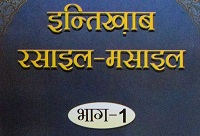
इंतिख़ाब रसाइल-मसाइल (भाग-1)
-
इस्लाम
- at 19 March 2024
रसाइल-मसाइल सवालों और उनके जवाबों का संग्रह है। महान लेखक और विद्वान मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी को पत्र लिखकर दुनिया भर से लोग सवाल पूछते रहते थे। मौलाना मौदूदी अपनी मासिक पत्रिका ‘तर्जमानुल-क़ुरआन’ में वे सवाल और उनके जवाब प्रकाशित कर देते थे। उन सवाल जवाब के महत्व को देखते हुए बाद में उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया और फिर उनका उर्दू से हिन्दी में अनुवाद भी किया गया। वे सवाल-जवाब इतने उपयोगी और प्रसांगिक हैं कि हम उन्हें आन लाइन पढ़नेवालों के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं। [-संपादक]
लेखक : मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी
अनुवाद : मुहम्मद आबिद हामिदी
प्रकाशक : मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स
Intekhab Rasael-Masael-1 [H] – MMI Publishers
“अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करनेवाला है।"
दो शब्द
मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (1903-1979) बीसवीं शताब्दी के मशहूर आलिमे-दीन और लेखक थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी इस्लाम के सच्चे पैग़ाम को लोगों तक पहुँचाने में लगा दी और इसके लिए बहुत-सी परेशानियाँ और मुसीबतें झेलीं। मौलाना ने इस्लाम के पैग़ाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए 100 से अधिक किताबें लिखीं जिनके देश-विदेश की 40 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।
मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) के लिखने का अन्दाज़ बहुत ही सादा मगर दिलनशीन था। उन्होंने जिस विषय पर भी लिखा उसका हक़ अदा किया। उनकी लिखी हुई किताबें और लेख आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 50 साल पहले थे। मौलाना मौदूदी ने सिर्फ़ किताबें ही नहीं लिखीं बल्कि उनपर ख़ुद अमल किया और लोगों को भी उनपर अमल कराने के लिए एक तहरीक की बुनियाद रखी जिसे भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश में जमाअते-इस्लामी के नाम से जाना जाता है।
मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) ने जब एक तहरीक (आन्दोलन) शुरू की और लोगों को इस्लाम की तरफ़ बुलाना शुरू किया तो लोगों ने अपनी रहनुमाई के लिए बहुत-से सवाल किए। मौलाना ने इन सवालों के तसल्ली-बख़्श जवाब दिए जिनको उर्दू के माहनामा तर्जमानुल-क़ुरआन में प्रकाशित किया जाता रहा। बाद में उन सभी सवालों को उनके जवाबों सहित 'रसाइल-व-मसाइल' के नाम से 6 हिस्सों में पुस्तक के रूप में छापा गया। यहाँ यह बात वाज़ेह रहे कि छठा हिस्सा जनाब मलिक ग़ुलाम अली के क़लम से है; अलबत्ता शुरु के पाँच हिस्से मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) ही के हैं।
वास्तविकता यह है कि न सिर्फ़ तहरीकी मसाइल को समझने के लिए बल्कि दीन की बुनियादी बातों को जानने और समझने के लिए भी 'रसाइल-व-मसाइल' बहुत-ही फ़ायदेमन्द साबित हुई है और आम लोगों में बड़ी पसन्द की गई है।
आम लोगों में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इस किताब का हिन्दी में तर्जमा कराया गया। यूँ तो इस किताब का हर सवाल अहम है लेकिन हमने हिन्दी में बहुत-ही अहम सवालों को 6 हिस्सों में से छाँटकर प्रकाशित किया है।
नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाही
सेक्रेट्री
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (दिल्ली)
अरबी क़ुरआन पर ग़ैर-अरब क्यों ईमान लाएँ?
सवाल
"हमने अपना पैग़ाम पहुँचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी क़ौम ही की ज़बान में पैग़ाम पहुँचाया है, ताकि वह उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए।” (क़ुरआन, 14:4)
इस आयत को पढ़कर यह सोचता हूँ कि हमारी और हमारे बाप-दादा की ज़बान (भाषा) अरबी नहीं थी। फिर क़ुरआन मजीद के अरबी होने पर हम क्यों पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैरवी पर मजबूर थे।
जवाब
आपका मतलब शायद यह है कि हर क़ौम को सिर्फ़ उसी दावत पर ईमान लाने पर मजबूर होना चाहिए जो उसकी अपनी ज़बान में दी गई हो। दूसरी किसी ज़बान में आई हुई दावत अगरचे वह हक़ (सत्य) हो, चाहे वह अल्लाह की जानिब से हो और चाहे वह तर्जमों, तफ़सीरों, तशरीहों और अमली नमूनों के ज़रिये से आप तक पहुँच जाए फिर भी उसकी पैरवी लाज़िम न होनी चाहिए, क्योंकि वह आपको अपनी ज़बान में नहीं भेजी गई है। अगर यही आपका मतलब है तो यह सिर्फ़ एक ग़लतफ़हमी है जो ऊपर लिखी आयत का सही मतलब न समझने से पैदा हो गई है। आयत का मक़सद अस्ल में यह है कि अल्लाह ने जब कभी किसी क़ौम में कोई रसूल भेजा है यह ख़याल किए बिना कि वह रसूल ख़ास उसी क़ौम के लिए हो या तमाम दुनिया के लिए, बहरहाल उसने सबसे पहले मुख़ातब लोगों को उनकी अपनी ज़बान ही में ख़िताब किया है ताकि वे उसकी बात को अच्छी तरह समझ सकें और उनको यह दलील पेश करने का मौक़ा न मिले कि "ज़बाने-यार मन तुर्की, व मन तुर्की नमी दानम" यानी मेरे दोस्त की ज़बान तो तुर्की है और मैं तुर्की नहीं समझता। इसका यह मतलब नहीं है कि हर क़ौम के लिए लाज़िमी तौर पर अलग एक नबी ही आना चाहिए जो उसको अपनी ज़बान ही में ख़िताब करे और न इसका मतलब यह है कि अगर एक क़ौम को दूसरी क़ौम के ईमानवाले उसकी अपनी ज़बान में समझने लायक़ तरीक़े से ख़ुदाई तालीम पहुँचा दें तब भी वह सिर्फ़ इस बुनियाद पर उसे रद्द कर देने में सही माना जाए कि नबी ख़ुद सीधे ख़ुदा की किताब उसकी ज़बान में लेकर नहीं आया है, यह बात न इस आयत में कही गई है और न इसके शब्दों में ऐसी कोई गुंजाइश है कि उससे यह नतीजा निकाला जा सके। आख़िर कौन-सी माक़ूल वजह इस बात के लिए पेश की जा सकती है कि जिस शख़्स को क़ुरआन मजीद की तालीम का निचोड़ उसकी अपनी ज़बान में साफ़-साफ़ पहुँच गया हो वह इसपर ईमान न लाने में अपने आप को सही समझता हो?
सवाल
एक सिख दोस्त को पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी गईं हैं। पढ़ने के बीच ही में उनकी तरफ़ से यह सवाल सामने आया कि तुम कहते हो कि ख़ुदा पैग़म्बरों से बात करता है और उसने अपने उन ख़ास बन्दों के ज़रिये से इनसानों के लिए एक हमागीर (व्यापक) निज़ामे-ज़िन्दगी भेजा है। सवाल यह है कि इतना अहम निज़ाम एक ऐसी ज़बान में क्यों पेश किया गया है जो एक ख़ास ज़मीन के हिस्से में बोली जाती है? क्यों न उस ख़ुदा ने, जो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है, सारी दुनिया के लिए एक ज़बान बना दी ताकि हर कोई उसके कलाम से समान रूप से फ़ायदा उठाता? अरबी क़ुरआन मजीद तो सिर्फ़ अरबों ही के लिए फ़ायदेमन्द है।
जवाब
आपके जिन सिख दोस्त ने यह एतिराज़ किया है वह अगर अपनी सोच को थोड़ी और गहराई तक ले जाते तो इससे बढ़कर वह यह सवाल भी कर सकते थे कि क़ुरआन की एक-एक कापी (प्रति) सीधे एक-एक आदमी के पास ख़ुदा ने क्यों नहीं भेजी। क्योंकि जब वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है तो ऐसा भी कर सकता है। [यह एतिराज़ बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह पुराने ज़माने के इनकार करनेवाले और मुशरिक करते थे कि नबी अगर सच्चा है तो उसके साथ बड़े-बड़े ख़ज़ाने क्यों नहीं हैं कि आराम की ज़िन्दगी बिताए और अपनी दावत को ख़ूब फैला सके? या नबी इनसान क्यों है और इनसानी ज़रूरतें और कमज़ोरियाँ क्यों रखता है? उसे तो फ़रिश्ता होना चाहिए और फ़ितरी ताक़तों से भी आगे बढ़कर अपनी दावत व तहरीक को फैलाना चाहिए।]
अस्ल में ये लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि अल्लाह ने इनसानों की हिदायत के लिए कोई ऐसा तरीक़ा नहीं अपनाया है जिससे दुनिया के इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत पेश आए जो अपनी फ़ितरी गति पर चल रहा है। इनसानों में ज़बान का इख़्तिलाफ़ (भिन्नता) और इस बुनियाद पर इनसानों में छोटे और बड़े समूह का बन जाना एक फ़ितरी चीज़ है जो ख़ुद अल्लाह ही के चाहने से वुजूद में आई है और इसमें बेशुमार मसलहतें हैं जिनको अल्लाह बरबाद नहीं करना चाहता। वह अगर क़ुदरत रखनेवाला है तो इसके साथ वह हिक्मतवाला भी है। उसकी सल्तनत का निज़ाम अटल नियमों पर चल रहा है। इन्हीं नियमों के तहत क़ौमों की ज़बानों (भाषाओं) और उनके रीति रिवाज तरह-तरह के बनते हैं। अगर 'इसप्रान्टो' की तरह की कोई ज़बान अल्लाह की तरफ़ से पैदा की जाती तब भी वह न तो क़ौमों की मादरी ज़बान (मात्र-भाषा) बन सकती थी न उसके अदब (साहित्य) से दिल मुतास्सिर हो सकते थे और न ही लोग उसकी अदबी नज़ाकतों (साहित्यिक सरसता) को महसूस (Appreciate) कर सकते थे। सिवाय इसके कि क़ौमों की मादरी ज़बानों को अल्लाह तआला ग़ैर-फ़ितरी तरीक़े से मिटा देता और ग़ैर-फ़ितरी तरीक़े ही से इस 'इसप्रान्टो' को ज़बरदस्ती तमाम क़ौमों की ज़बान बना देता। चूँकि अल्लाह का एक काम उसके दूसरे काम को मिटाने के लिए नहीं होता इस वजह से अल्लाह ने इनसानी ज़बानों के पिछले निज़ाम (व्यवस्था) को बरक़रार रखते हुए इनसानों की हिदायत का काम अंजाम दिया है।
यह सवाल कि अरबी में क़ुरआन मजीद सिर्फ़ अरबों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसी सूरत में सही हो सकता था जबकि अल्लाह ने सिर्फ़ किताब उतारी होती। लेकिन हक़ीक़त यह है कि अल्लाह ने अपनी किताब के साथ-साथ रहनुमा भी पैदा किया। उस रहनुमा ने पहले इनसानों की एक क़ौम को, जिसकी ज़बान में किताब उतारी गई थी, ख़िताब (सम्बोधित) किया। फिर उस क़ौम को तालीम-तज़्किया, अमली तरबियत और कामिल इज्तिमाई इंक़िलाब के ज़रिये से उस निज़ाम के साँचे में ढाल दिया जो किताब के मंशा के मुताबिक़ था। फिर उस क़ौम के हवाले यह ख़िदमत की कि वह दुनिया की दूसरी क़ौमों को नबी का नायब बनकर उसी तरह ख़िताब करे और उसी तरह तालीम व तज़्किया, अमली तरबियत और पूर्ण इज्तिमाई इंक़िलाब के ज़रिये से उस साँचे में ढालने की कोशिश करे जिसमें पहले वह ख़ुद ढाली गई थी। फिर जो-जो क़ौमें इस तरीक़े से असर को क़बूल करती जाएँ वे दूसरी क़ौमों के लिए यही ख़िदमत अंजाम दें। यह उस तालीम को आम करने का फ़ितरी तरीक़ा था, और दुनिया में जिस-जिस तहरीक (जमाअत) ने भी तमाम इनसानों तक दावत पहुँचाने का काम किया है चाहे वह तहरीक ख़ुदापरस्ती की हो या किसी दूसरी क़िस्म की हरहाल में उसने फ़ितरतन यही रास्ता अपनाया है।
अगर यह उसूल क़बूल कर लिया जाए कि कोई किताब सिर्फ़ उसी क़ौम के लिए फ़ायदेमन्द है जिसकी ज़बान में वह लिखी गई हो तो फिर दुनिया के इल्मी (ज्ञानात्मक) इतिहास को ग़लत तस्लीम करना पड़ेगा। फिर तो इनसानों की लिखी हुई किताबों को भी ज़बानों (भाषाओं) के लिहाज़ से क़ौमों के लिए ख़ास कर देना होगा और तर्जमों और सारे इनसानों तक तबलीग़ करने के तमाम दूसरे साधनों के फ़ायदा उठाने से इनकार कर देना होगा। जबकि यही चीज़ें हैं जिनके बल पर बड़ी-बड़ी तहरीकों की दावत और बड़ी-बड़ी हस्तियों के पैग़ाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलते रहे हैं। फिर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पेश की हुई किताब ही ने क्या क़ुसूर किया है कि महज़ अरबी ज़बान में होने की वजह से उसे अरब क़ौम के लिए ही मख़सूस (विशिष्ट) और महदूद (सीमित) कर दिया जाए।
अगर कोई शख़्स इस चीज़ से मुतमइन न हो और बराबर अपनी उस हठ पर क़ायम रहे कि जो कुछ वह चाहता है उसी तरह अल्लाह को करना चाहिए था तो उसे अपनी राय पर जमे रहने का पूरा हक़ हासिल है, मगर सवाल यह है कि ऐसे-ऐसे सवालों को रास्ते का रोड़ा बनाकर अगर एक शख़्स एक किताब या एक पैग़ाम से फ़ायदा उठाना नहीं चाहता तो नुक़सान किसका है? यह रवैया हक़ और सच्चाई के चाहनेवालों का नहीं होता। वे तो जगह-जगह टोह लगाते फिरते हैं कि सच्चाई की रौशनी कहाँ है और कहाँ से वह मिलती है। अगर आदमी दुनिया की हर किताब, हर पैग़ाम और हर तालीम के मुक़ाबले में अपने दिलो-दिमाग़ पर किसी न किसी क़िस्म का ताला चढ़ा ले तो फिर वह एक क़दम भी ज़िंदगी की सीधी राह पर नहीं चल सकता।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जुलाई-अक्तूबर, 1944 ई.)
खुदा है या नहीं, है तो कहाँ से आया?
सवाल
कुछ समय पहले की बात है, एक दोस्त के साथ मेरी बहस हो गई। सवाल यह था कि ख़ुदा है या नहीं? और अगर है तो वह कहाँ से आया। हम दोनों इस मामले में इल्म नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी मैं सवाल के पहले हिस्से की हद तक अपने दोस्त को मुतमइन करने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे हिस्से का कोई जवाब मुझसे बन नहीं आया। चुनांचे अब यह सवाल ख़ुद मुझे परेशान कर रहा है।
एक मौक़े पर मेरी नज़र से यह बात गुज़री है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से भी यह सवाल किया गया था और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसके जवाब में फ़रमाया था कि कुछ बातें इनसान के सोचने और समझने से बाहर होती हैं, और यह सवाल भी उन्हीं में शामिल है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस फ़रमान से इतमीनान हासिल करूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। मेहरबानी करके आप मेरी मदद फ़रमाएँ।
मेरा दूसरा सवाल यह है कि इनसान को सही मानों में इनसान बनने के लिए किन-किन उसूलों पर चलना चाहिए?
जवाब
आपके ज़ेहन को जिस सवाल ने परेशान कर रखा है उसका हल तो किसी तरह मुमकिन नहीं है। अलबत्ता आपकी परेशानी का हल ज़रूर मुमकिन है और उसकी सूरत यह है कि आप इस तरह के मसलों पर सोचने की तकलीफ़ उठाने से पहले अपने इल्म (ज्ञान) की हदों (Limitations) को अच्छी तरह से समझ लें। जब आप यह जान लेंगे कि इनसान क्या कुछ जान सकता है और क्या कुछ नहीं जान सकता तो फिर आप बेकार में ऐसी बातों को जानने की कोशिश में न पड़ेंगे जिनको जानना आपके बस में नहीं है। ख़ुदा की हस्ती के बारे में ज़्यादा-से-ज़्यादा जो कुछ आदमी के बस में है वह सिर्फ़ इतना है कि कायनात की निशानियों पर ग़ौर करके एक नतीजा निकाल सके कि ख़ुदा है और उसके सभी काम गवाही देते हैं कि उसके अन्दर ये और ये गुण होने चाहिएँ। यह नतीजा भी ‘इल्म' की हैसियत नहीं रखता बल्कि सिर्फ़ एक अक़्ली क़यास और पक्के यक़ीन की हैसियत रखता है। इस क़यास और गुमान को जो चीज़ पक्का करती है वह यक़ीन और ईमान है। लेकिन कोई साधन हमारे पास ऐसा नहीं है जो उसको इल्म की हद तक पहुँचा सके। अब आप ख़ुद सोच लीजिए कि जब ख़ुदा की हस्ती के बारे में भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम को उसके होने का इल्म हासिल है, तो आख़िर उसकी हक़ीक़त का तफ़सीली इल्म किस तरह मुमकिन है? ख़ुदा की हस्ती तो बहुत ही बुलंद और बरतर है, हम तो यह भी नहीं जानते कि 'ज़िन्दगी' की हक़ीक़त और उसकी अस्ल (Origin) क्या है। यह शक्ति (ऊर्जा, Energy) जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी ने माद्दे की सूरत अपनाई है और इससे यह कायनात (सृष्टि) वुजूद में आई है, इसकी हक़ीक़त हमें नहीं मालूम, और न हम यह जानते हैं कि यह कहाँ से आई और किस तरह इसने माद्दे (तत्व) की अलग-अलग शक्लें अपना लीं। इस तरह के मामलों में 'क्यों' और 'कैसे' के सवालों पर ग़ौर करना अपनी अक़्ल और ज़ेहन को उस काम की तकलीफ़ देना है जिसके अंजाम देने की ताक़त और साधन उसको हासिल ही नहीं हैं। इसलिए यह चिन्तन-मनन न पहले कभी इनसान को किसी नतीजे पर पहुँचा सका है, न अब आपको पहुँचा सकता है। इसका हासिल सिवाए हैरानी के और कुछ नहीं। इसके बजाय अपने ज़ेहन और अक़्ल को उन सवालों पर मरकूज़ (केन्द्रित) कीजिए जिनका ताल्लुक़ आपके जीवन से है और जिनका समाधान सम्भव है। यह सवाल तो बेशक हमारी ज़िन्दगी से ताल्लुक़ रखता है कि ख़ुदा है या नहीं, और है तो उसके गुण क्या-क्या हैं, और इसके साथ हमारा ताल्लुक़ किस क़िस्म का है? इस मामले में कोई न कोई राय (मत) अपनानी ज़रूरी है। क्योंकि बग़ैर इसके हम ख़ुद अपनी ज़िन्दगी का रास्ता मुतय्यन (निश्चित) नहीं कर सकते और इस मामले में एक राय क़ायम करने के लिए काफ़ी साधन भी हमें हासिल हैं। लेकिन यह सवाल कि "ख़ुदा कहाँ से आया" न हमारे जीवन के मसलों से कोई ताल्लुक़ रखता है और न उसके बारे में किसी नतीजे पर पहुँचने के साधन हमको हासिल हैं।
आपका दूसरा सवाल कि "इनसान को इनसान बनने के लिए किन उसूलों और नियमों पर चलना चाहिए" ऐसा नहीं है कि इसका जवाब एक ख़त में दिया जा सके। मैं अपनी किताबों में इसके अनेक पहलुओं पर तफ़सील से लिख चुका हूँ। आप उनको पढ़ लें। मिसाल के तौर पर इसके लिए मेरे लेख 'शन्ति मार्ग', 'इस्लाम और अज्ञान', 'इस्लाम का नैतिक दृष्टिकोण' और 'सत्य धर्म' को पढ़ लेना फ़ायदेमन्द होगा। 'रिसाल-ए-दीनयात' से भी आपको इस मामले में काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। (तर्जमानुल-क़ुरआन, अक्तूबर 1950 ई.)
अल्लाह के वुजूद के बारे में एक सवाल
सवाल
नीचे लिखा सवाल मेरे दोस्त के दिमाग़ में एक लम्बे समय से खटक रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सही जवाब न दे सका। उम्मीद है कि जवाब देकर शुक्रिया का मौक़ा देंगे।
"अल्लाह कैसे वुजूद में आया? जबकि हर मौजूद चीज़ के लिए अक़ली तौर पर किसी मूजिद (बनानेवाले) का होना निहायत ज़रूरी है।"
जवाब
जिस तरह अक़्ल यह चाहती है कि किसी वुजूद के लिए एक मूजिद (बनानेवाला) हो, उसी तरह अक़्ल यह भी चाहती है कि सारी कायनात का बनानेवाला (मूजिद) कोई ऐसा वुजूद हो जो किसी मूजिद के बग़ैर आप से मौजूद हो, वरना हर मौजूद के लिए एक मूजिद दरकार होगा और यह सिलसिला कहीं जाकर न रुकेगा। ख़ुदा तो कहते ही उसको हैं जो सबका पैदा करनेवाला (ख़ालिक़) हो और ख़ुद किसी का पैदा किया हुआ (मख़लूक़) न हो। अगर वह मख़लूक़ हो तो वह ख़ुदा न होगा, बल्कि जिसने उसको पैदा किया हो वही ख़ुदा होगा।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, नवम्बर 1965)
कुछ आधुनिक नास्तिकतावादी नज़रियों का इल्मी जाइज़ा
सवाल
मेरे एक नातेदार जो एक ऊँचे सरकारी ओहदे पर हैं, किसी ज़माने में पक्के दीनदार और नमाज़-रोज़े के पाबन्द हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ किताबें पढ़कर मज़हब के इनकारी हो गए हैं। उनके विचार बिल्कुल बदल चुके हैं। अब तो वे अपने उन विचारों को दूसरों तक पहुँचाने और फैलाने से भी बाज़ नहीं आते। मैं उनके मुक़ाबले में इस्लामी हुक्मों और तालीमात की हिफ़ाज़त की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अपनी कमइल्मी की वजह से दलीलों के साथ उनको जवाब देना मेरे बस में नहीं है। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि मेरी मदद फ़रमाएँ। मोटे तौर पर उनके नज़रियात इस तरह हैं—
(1) ख़ुदा को वे हर क़ुदरत रखनेवाला और इस संसार का पैदा करनेवाला तो मानते हैं, मगर उनके मुताबिक़ संसार को ख़ुदा ने बनाकर छोड़ दिया है और अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप-से-आप (Automatic) हो रहा है।
(2) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को वे एक समाज सुधारक (रीफ़ार्मर) से ज़्यादा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता उन्हें वे एक नेक और ग़ैर मामूली क़ाबिलियत का इनसान भी समझते हैं।
(3) क़ुरआन मजीद को वे (अल्लाह की पनाह) ख़ुदा के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का लिखा हुआ मानते हैं। इसकी बहुत-सी बातों को इस वजह से अमल के क़ाबिल नहीं समझते हैं कि वे सिर्फ़ उस वक़्त के लिए थीं, जब क़ुरआन नाज़िल हुआ था।
(4) इबादतों नमाज़-रोज़ा वग़ैरा को सिर्फ़ बुराई से बचने का बेहतरीन ज़रीआ और समाज को सही डगर पर चलाने का साधन समझते हैं।
(5) शैतानी नज़रिया, उनके ख़याल में, ख़ुदा के वास्ते एक चेलैंज की हैसियत रखता है क्योंकि ख़ुदा तो नेकी की तौफ़ीक़ देता है और शैतान बुराई की तरफ़ खींचता है। देखने में तो आमतौर पर शैतान की जीत होती है।
(6) चार शादियों, ग़ुलाम रखने और क़ुरबानी को बेकार मानते हैं।
उम्मीद है कि आप कुछ वक़्त निकालकर इन बातों का संक्षेप में जवाब देंगे और उन किताबों के नाम जहाँ से मैं उनकी तसल्ली कर सकूँ लिख कर शुक्रिए का मौक़ा देंगे।
जवाब
मुझे आपके सरकारी ओहदे पर बैठे रिश्तेदार के विचारों को मालूम करके बड़ा दुख और अफ़सोस हुआ, अल्लाह उनको हिदायत दे और आपको उनके असर से महफ़ूज़ रखे। अगर आपने मेरी किताबों का मुताला (अध्ययन) किया होता तो आप उनकी सभी बातों का जवाब बड़ी अच्छी तरह दे सकते थे। अब भी मैं आपको मुताला करके तैयार रहने का मशविरा दूँगा। क्योंकि पत्राचार के द्वारा इतने बड़े-बड़े मसलों को समझाना बड़ा मुश्किल है।
संक्षेप में उन बातों का जवाब देता हूँ, जो आपने पूछी हैं—
(1) सबसे पहली बात यह है कि जिस शख़्स की सोचने की ताक़त ख़राब न हुई हो वह कभी यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई क़ानून और व्यवस्था (Law and Order) किसी लागू करनेवाले इक़ितदार (Authority) के बग़ैर भी लागू हो सकती है और जारी रह सकती है। कायनात में क़ानून और व्यवस्था मौजूद है, इसका इनकार तो किसी तरह किया ही नहीं जा सकता। अब क्या अक़्ल यह मान सकती है कि इतने बड़े लामहदूद पैमाने पर लामहदूद मुद्दत तक यह क़ानून और व्यवस्था किसी इक़्तिदार (सत्ता) के बग़ैर ही चल रही है? तास्सुब (पक्षपात) न रखनेवाली कोई भी अक़्ल इसे मान नहीं सकती। मगर दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से अच्छे-ख़ासे होशमन्द इनसान इस नादानी में फँस जाते हैं। एक यह कि उनके सोच-विचार की सलाहियत बहुत तंग होती है जिसकी वजह से वे उस अज़ीमुश्शान (महान) इक़ितदार के बारे में सोचने में नाकाम रह जाते हैं जो इतनी बड़ी कायनात में क़ानून और व्यवस्था को शुरू से अब तक चला रहा है। दूसरे यह कि वह इसको मानना चाहते ही नहीं हैं क्योंकि उसके मान लेने के बाद उनके लिए दुनिया में मनमानी करने की आज़ादी बाक़ी नहीं। रहती।
यह तो ख़ुदा के बारे में उनके तसव्वुर की ग़लती है, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे पूछिए कि इतने बड़े-बड़े मसलों पर सोचने और राय ज़ाहिर करनेवाले आदमियों को कम-से-कम ईमानदार (Honest) तो होना चाहिए। आप लोग तो इस ख़ूबी से भी ख़ाली हैं। आप ख़ुदा, रसूल और क़ुरआन के बारे में जो बातें करते हैं वे इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मगर इसके बावुजूद आप मुसलमान बने फिरते हैं और मुस्लिम समाज को धोखा देने में ज़रा भी नहीं झिझकते। अगर आप ईमानदार होते तो जिस वक़्त आप ने अपनी ये राएँ क़ायम की थीं उसी वक़्त इस्लाम से अपने अलग होने का एलान कर देते और अपना नाम भी बदल लेते, ताकि मुस्लिम समाज आपसे धोखा खाकर आपके साथ वे मामलात जारी न रखता जो वह किसी ग़ैर-मुस्लिम के साथ रखना पसन्द नहीं करता। इस खुली जालसाज़ी और फ़रेब के बाद आपकी किसी राय को वह अहमियत देना जो सिर्फ़ ईमानदार और सच्चे लोगों की रायों ही को दी जा सकती है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है।
(2) रसूल के बारे में उनके ख़याल और विचार मुतज़ाद (विरोधाभासी) हैं। एक तरफ़ वे रसूल को नेक आदमी भी कहते हैं जिससे लाज़िम आता है कि वे उसको सच्चा आदमी भी मानें (अलावा इसके कि उनके नज़दीक कोई झूठा आदमी भी नेक हो सकता है) और दूसरी तरफ़ वे रसूल के उस दावे को झूठ भी क़रार देते हैं कि वह सिर्फ़ रीफ़ार्मर (प्रवर्तक) नहीं है बल्कि ख़ुदा की तरफ़ से रसूल बनाकर भेजा गया है। एक सही अक़्ल रखनेवाला आदमी इन दोनों बातों को जमा नहीं कर सकता। उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तेईस साल तक अपनी ज़िन्दगी का हर लमहा अपने विरोधियों के मुक़ाबले में एक ऐसी जिद्दोजुहद (Struggle) करते हुए गुज़ारा है, जिसकी बुनियाद ही यह थी कि आप अपनी रिसालत के दावेदार थे और आप के विरोधी इस बात को मानना नहीं चाहते थे। अब एक आदमी के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में दो ही रवैये अपनाना अक़्ल के मुताबिक़ हो सकता है। एक यह कि अगर वह उनको सच्चा आदमी समझता है तो उनको रसूल माने। दूसरे यह कि अगर वह उनको रसूल नहीं मानता तो (अल्लाह की पनाह) उन्हें बेहद झूठा और फ़रेब देनेवाला समझे। इन दोनों बातों के बीच एक तीसरी राह अपनाना और यह कहना कि वे सच्चे आदमी भी थे और रसूल भी न थे, सरासर अक़्ल के ख़िलाफ़ बात है।
इसके जवाब में ऐसे लोगों की तरफ़ से ज़्यादा से ज़्यादा दो बातें कही जा सकती हैं। एक यह कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने महज़ इस्लाह (सुधार) की ख़ातिर रिसालत का दावा कर दिया ताकि वे ख़ुदा के नाम से वे हुक्म मनवा सकें जो वे अपने नाम से पेश करके न मनवा सकते थे। दूसरे यह कि वे अपने उस दावे में सच्चे तो थे मगर हक़ीक़त में रसूल न थे बल्कि इस ग़लतफ़हमी में पड़े हुए थे कि वे रसूल हैं।
इनमें से पहली बात जो आदमी कहता है वह मेरे नज़दीक अख़लाक़ी (नैतिक) हैसियत से बड़ा ख़तरनाक आदमी है जिससे हर शरीफ़ इनसान को होशियार रहना चाहिए। इसलिए कि अगर हम उसके इस ख़याल का जाइज़ा लें तो यह साफ़ मालूम होता है कि उस आदमी के नज़दीक नेक मक़सद के लिए काम करने का बुरा तरीक़ा अपनाना न सिर्फ़ यह कि जाइज़ है बल्कि एहतिराम के क़ाबिल (Respectable) भी है। इसी वजह से वह ऐसे आदमी को सुधारक और नेक आदमी समझता है जिसने उसके ख़याल में महज़ सुधार करने के लिए (अल्लाह की पनाह) रिसालत का दावा जैसा बहुत बड़ा फ़रेब गढ़ लिया था। इस तरह के घटिया नज़रिए रखनेवाले आदमी से कुछ मुश्किल नहीं है कि कल वह किसी अच्छे मक़सद के लिए (जिसको वह अच्छा समझता हो) किसी के यहाँ चोरी कर डाले, या कोई जाली दस्तावेज़ (ग़ैर-क़ानूनी लेखा-जोखा) बना ले, या और किसी घिनावने अख़लाक़ी जुर्म का करनेवाला हो जाए। क्योंकि जब उसके नज़दीक एक फ़रेबी इस बुनियाद पर नेक और सुधारक हो सकता है कि उसने सुधार के लिए फ़रेबकारी की है, तो आख़िर वह ख़ुद अच्छे मक़सदों के लिए जुर्म करने से कब बाज़ रह सकता है।
दूसरी बात जो आदमी कहता है वह अक़्ली हैसियत से उतना ही गिरा हुआ है जितना ऊपरवाली बात कहनेवाला अख़लाक़ी हैसियत से गिरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा छूट (Allowance) देते हुए ऐसे आदमी के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वह यह है कि यह आदमी बहुत बड़े मसलों पर भी बहुत कम सोच-विचार करके राय ज़ाहिर कर देने का मरीज़ है। इसलिए कि अगर वह इस कम-अक़्ली में ग्रस्त न होता तो कभी इस बात को मुमकिन ख़याल न करता कि एक आदमी इतना बुद्धिमान और सूझ-बूझवाला भी हो कि उसे इनसानी इतिहास के बुलन्दतरीन और कामयाब-तरीन लीडरों में शुमार करने से उसके विरोधी भी इनकार न कर सकें और दूसरी तरफ़ वह अपने बारे में तेईस साल तक लगातार इतनी बड़ी ग़लतफ़हमी में पड़ा रहे और अपना सारा काम उसी ग़लतफ़हमी की बुनियाद पर चलाता रहे। बल्कि आए दिन क़ुरआन मजीद की पूरी-पूरी सूरतें ख़ुद लिख करके दुनिया को सुनाता रहे और फिर भी इस ग़लतफ़हमी में पड़ा हुआ हो कि ये सूरतें मेरे ऊपर ख़ुदा की तरफ़ से नाज़िल (अवतरित) हो रही हैं। मेरे नज़दीक तो इस बात को मुमकिन और माक़ूल (बुद्धिसंगत) समझनेवाले आदमी की अपनी अक़्ल ही मुश्तबा (सन्दिग्ध) है, उसकी अक़्ल सही होती तो वह ख़ुद जान लेता कि इस तरह की ग़लतफ़हमी सिर्फ़ पागल व मजनून आदमियों को हुआ करती है, और किसी पागल आदमी से वे कमाल दर्जे के अक़्ल और इल्म से भरे कारनामे ज़ाहिर नहीं हो सकते जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से ज़ाहिर हो रहे हैं।
(3) क़ुरआन मजीद के बारे में उनके जो ख़यालात आपने नक़ल किए हैं उनके बारे में भी मेरी वही राय है जो मैंने ऊपर अर्ज़ की है कि वे किसी चीज़ से पूरी जानकारी हासिल किए बग़ैर और उसपर काफ़ी सोच-विचार किए बग़ैर राय क़ायम करने के आदी हैं। उनसे पूछिए कि आपने सारी उम्र में कितनी बार क़ुरआन का गहरा, तहक़ीक़ी मुताला किया है, जिसके बाद आप इस बारे में यह फ़ैसला देने के क़ाबिल हुए हैं। अगर वे ईमानदारी के साथ यह क़बूल कर लें कि उन्होंने इस तरह का तहक़ीक़ी मुताला नहीं किया है तो उनसे गुज़ारिश कीजिए कि तहक़ीक़ के बग़ैर ऐसे अहम मसलों में फ़ैसला सादिर करना किसी होशमन्द और अक़्लमन्द पढ़े-लिखे आदमी की शान के मुताबिक़ नहीं है। अगर उनका दावा यह हो कि उन्होंने ख़ूब तहक़ीक़ करके यह राय क़ायम की है तो उनसे पूछिए कि क़ुरआन के अन्दर उन्होंने वह कौन-सी गवाही और दलील पाई है जिसे देखकर वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपना कलाम (कथन) है और यह भी पूछिए कि क़ुरआन की किन-किन बातों को उन्होंने अमल के लायक़ नहीं पाया या फिर क़ुरआन के नाज़िल होने के ज़माने तक के लिए अमल के लायक़ पाया है। इन बातों का तअय्युन (निर्धारण) उनसे करा लीजिए और फिर मुझे लिखिए ताकि मैं भी कुछ उनकी तहक़ीक़ के नतीजों से फ़ायदा उठा सकूँ।
(4) इबादतों (उपासना) के बारे में उनके जो नज़रियात आपने बयान किए हैं वे भी उनकी निहायत उलझी हुई सोच (Confused thinking), बल्कि बेफ़िक्री का नमूना हैं। शायद उन्होंने कभी इस बात पर ग़ौर नहीं किया कि नमाज़, रोज़ा वग़ैरह सभी अमल सिर्फ़ उसी सूरत में बुराई से बचने का बेहतरीन ज़रीआ और समाज को सही डगर पर चलाने का साधन हो सकते हैं जबकि उन्हें साफ़ दिल के साथ किया जाए और ख़ुलूस के साथ आदमी उनपर उसी सूरत में कारबन्द हो सकता है जब वह ईमानदारी से यह समझता हो कि ख़ुदा है और मैं उसका बन्दा हूँ और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं। और कोई आख़िरत आनेवाली है जिसमें मुझे अपने आमाल (कर्मों) का हिसाब देना है। लेकिन अगर कोई आदमी इन सब बातों को सच्चाई के ख़िलाफ़ समझता हो और यह ख़याल करता हो कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (अल्लाह की पनाह) महज़ सुधार के लिए यह ढोंग रचाया है, तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत में भी ये इबादतें बुराई से बचने का ज़रीआ और समाज को सही डगर पर चलाने का आला (यंत्र) बन सकेंगी। एक तरफ़ इन इबादतों के ये फ़ायदे बयान करना और दूसरी तरफ़ इन फ़िक्री (वैचारिक) बुनियादों को ख़ुद ढा देना जिनपर इन इबादतों के ये फ़ायदे मुनहसिर (निर्भर) हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी कारतूस से सारा गन पाउडर निकाल दें और फिर कहें कि यह कारतूस शेर के शिकार में बहुत कारगर है।
(5) शैतान के मसले पर उनका एतिराज़ देखकर साफ़ मालूम होता है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में कभी एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि क़ुरआन मजीद इनसान और शैतान के मामले में क्या हक़ीक़त बयान करता है। इसको जाने बग़ैर उन्होंने बस कुछ सुनी-सुनाई बातों की बुनियाद पर इस मसले का सतही-सा तसव्वुर क़ायम कर लिया और इसपर एतिराज़ जड़ दिया। यह एतिराज़ हक़ीक़त में उनकी अपनी ही सोच की बुनियाद पर है। उस तसव्वुर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता जो क़ुरआन मजीद ने पेश किया है। क़ुरआन मजीद का पेश किया हुआ तसव्वुर यह है कि ख़ुदा ने इनसान को एक महदूद (सीमित) क़िस्म की आज़ादी और ख़ुदमुख़तारी देकर इस दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है और शैतान को ख़ुद उसकी अपनी माँग पर आज़ादी दी है कि वह इस इम्तिहान में इनसान को नाकाम करने के लिए जो कोशिश करना चाहे कर सकता है। शर्त यह है कि वह सिर्फ़ भड़काने और लालच की हद तक हो। ताक़त के बल पर अपने रास्ते पर खींच ले जाने के इख़्तियारात उसे नहीं दिए गए हैं। इसके साथ अल्लाह ने ख़ुद भी इनसान को जबरन सही रास्ते पर चलाने से परहेज़ किया है और सिर्फ़ इस बात को काफ़ी समझा है कि इनसान के सामने नबियों तथा किताबों के ज़रिये से हक़ ((सत्य) की राह को पूरी तरह वाज़ेह कर दिया जाए। इसके बाद ख़ुदा की तरफ़ से आदमी को यह इख़्तियार हासिल है कि वह चाहे तो ख़ुदा के बताए हुए रास्ते को अपने लिए चुन ले और उसपर चलने का फ़ैसला करे और चाहे तो शैतान के दिए हुए लालच और तर्ग़ीबात (प्रेरणाओं) को क़बूल कर ले और उस रास्ते में अपनी कोशिशें और मेहनतें लगाने पर आमादा हो जाए जो शैतान उसके सामने पेश करता है। इन दोनों रास्तों में से जिसको भी ख़ुद इनसान अपने लिए चुनता है अल्लाह तआला उसी पर चलने के मौक़े उसे दे देता है। क्योंकि इसके बग़ैर इम्तिहान के तक़ाज़े पूरे नहीं हो सकते। इस पोज़ीशन को अच्छी तरह समझ लेने के बाद बताइए कि शैतान का चैलेंज अस्ल में किसके लिए है, ख़ुदा के लिए या इनसान के लिए? और इनसानों में से जो लोग शैतान की राह पर जाते हैं उनके मामले में शैतान की जीत ख़ुदा पर होती है या इनसान पर? ख़ुदा ने इनसान को और शैतान को आज़ादी के साथ कुश्ती लड़ने का मौक़ा दिया है और बता दिया है कि आदमी जीतेगा तो जन्नत में जाएगा और शैतान जीतेगा तो हारनेवाला आदमी और उसको ग़लत रास्ते पर ले जानेवाला शैतान दोनों जहन्नम में जाएँगे। अब क्या आप यह चाहते हैं कि ख़ुदा उसके मुक़ाबले में दख़ल देकर जबरन इनसान को कामयाब कराए।
(6) चार शादियों, ग़ुलामी और क़ुरबानी के बारे में मुख़्तसर तरीक़े से कुछ कहना मुश्किल है। मैं इन सभी मसलों पर कई बार बहुत ही तफ़सील के साथ अपने विचार ज़ाहिर कर चुका हूँ। बहुविवाह के मसले को समझने के लिए आप मेरी तफ़्सीर तफ़हीमुल क़ुरआन, भाग एक से इन मसलों के बारे में इंडेक्स की मदद से (निकाह, इस्लामी क़ानून और वैवाहिक जीवन के तहत) मुताला करें। इसके अलावा हुकूमत के बनाए हुए मैरेज कमीशन के सवालनामे का जो जवाब मैंने दिया था उसमें भी इस मसले पर बहस मौजूद है।
ग़ुलामी के मसले पर आप मेरे नीचे लिखे लेखों का मुताला करें—
(1) रसाइल व मसाइल, भाग-1 — "मैदाने जंग में क़हबागिरी"
(2) रसाइल व मसाइल, भाग-2 “इस्लाम में ग़ुलामी को ममनूअ क्यों न कर दिया गया?"
(3) तफ़हीमात, भाग-2 “ग़ुलामी का मसला" और "ग़ुलामों और लौंडियों के मुताल्लिक़ चन्द सवालात"
(4) तफ़हीमुल-क़ुरआन, भाग-1, 2 इंडेक्स में "ग़ुलामी” के उनवान के तहत पेजों के हवाले मौजूद हैं।
(5) माहनामा “तर्जमानुल-क़ुरआन" शुमारा जून 1956 ई. "कनीज़ की तारीफ़ और उसके हलाल होने की दलील, तअद्दुदे इज़्दिवाज और लैंडियाँ”
क़ुरबानी के बारे में आप मेरी किताब तफ़हीमात, भाग-2 में क़ुरबानी के बारे में मज़मून (लेख), और मेरा रिसाला "मसलए-क़ुरबानी" का मुताला करें।
इन सारी तहरीरों से, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको समझने-समझाने में बड़ी मदद मिलेगी।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जून 1962 ई.)
हजरे-असवद और काबा के बारे में ग़ैर-मुस्लिमों की ग़लतफ़हमियाँ
सवाल
यहाँ (इस्लामिक कल्चर सेंटर लन्दन में) कुछ अंग्रेज़ लड़कियाँ जुमा के दिन आई हुई थीं। बड़े ग़ौर से नमाज़ियों को नमाज़ पढ़ते देखती रहीं। बाद में उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप लोग दक्षिण-पूर्व की तरफ़ मुँह करके कयों नमाज़ पढ़ते हैं? किसी और तरफ़ क्यों नहीं करते? काबा को क्यों इतनी अहमियत देते हैं? हजरे-असवद (काला-पत्थर) को क्यों चूमते हैं? वह भी तो एक पत्थर है जैसे दूसरे पत्थर। इस तरह तो यह भी हिन्दुओं ही की तरह मूर्तिपूजा हो गई। वे सामने मूर्ति रखकर पूजते हैं और मुसलमान उसकी तरफ़ मुँह करके सजदा करते हैं। हम उन्हें तसल्लीबख़्श जवाब न दे सके। मेहरबानी करके हमें इसके बारे में कुछ बताएँ ताकि फिर ऐसा कोई मौक़ा आए तो हम सवाल करनेवालों को समझा सकें।
जवाब
तक़रीबन इसी तरह के कई सवाल भारत के कई हिस्सों से भी हमारे पास आए हैं। इससे अन्दाज़ा होता है कि आजकल जगह-जगह यह सवाल मुसलमानों के सामने छेड़ा जा रहा है। इन सवाल करनेवालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका मक़सद किसी न किसी तरह इस्लाम पर एतिराज़ जड़ना होता है और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जवाब भी तसल्लीबख़्श नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में हक़ीक़त को न जानने की वजह से नेक-नीयती के साथ शंकाएँ पैदा होती हैं। ऐसे लोगों के लिए यह बात बिल्कुल काफ़ी है कि आप उन्हें माक़ूलियत के साथ हक़ीक़त से आगाह कर दें।
मूर्तिपूजा (बुत-परस्ती) की हक़ीक़त यह है कि मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के मुख़्तलिफ़ गिरोह यह समझते हैं कि ख़ुदा के साथ कुछ दूसरी हस्तियाँ भी ख़ुदाई सिफ़तें और इख़्तियार रखती हैं या यह ख़याल करते हैं कि अल्लाह उनके अन्दर समाहित हो गया है, और इस ग़लत अक़ीदे की बुनियाद पर वे उन हस्तियों की मूर्तियाँ और मन्दिर बनाकर उनके आगे पूजा-पाठ की रस्में अदा करते हैं। ख़ुद अल्लाह की मूर्ति आज तक किसी बहुदेववादी क़ौम ने नहीं बनाई है। और न उसकी पूजा-उपासना के लिए कभी यह तरीक़ा अपनाया गया है कि उसकी कोई ख़याली शक्ल तैयार करके उसके आगे माथा टेकते हों। दुनिया भर के तमाम बहुदेववादी क़रीब-क़रीब साफ़ तौर पर यह समझते रहे हैं कि अल्लाह तआला की कोई शक्ल व सूरत नहीं है। उसका और दूसरे माबूदों (उपास्यों) का फ़र्क़ उनके अक़ीदों और मज़हबी रीति-रिवाजों में साफ़ तौर से स्वीकार किया गया है। इसी लिए मूर्ति केवल दूसरे माबूदों ही की बनाई गई है। अल्लाह को इससे अलग रखा गया है। मूर्तिपूजा की इस हक़ीक़त को जो शख़्स भली-भाँति समझ लेगा वह इस ग़लतफ़हमी में नहीं पड़ सकता कि मुसलमानों का नमाज़ में काबा की ओर रुख़ करना या हज में काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) करना और हजरे-असवद (काले पत्थर) को चूमना मूर्तिपूजा से कोई मामूली-सी समानता भी है। इस्लाम एक ख़ालिस तौहीदी (एकेश्वरवादी) धर्म है जो अल्लाह के सिवा सिरे से किसी को ख़ुदा नहीं मानता और न ही इस बात का क़ायल है कि अल्लाह किसी के अन्दर समाहित हुआ है या वह किसी माद्दी मख़लूक़ की शक्ल में अपने आपको ज़ाहिर करता है। काबा को अगर ग़ैर-मुस्लिमों ने नहीं देखा है तो उसकी तस्वीरें तो ज़रूर उन्होंने देखी ही हैं। क्या वे ईमानदारी के साथ यह कह सकते हैं कि यह अल्लाह की मूर्ति है जिसकी मुसलमान उपासना कर रहे हैं? क्या कोई शख़्स सही होश व हवास रखते हुए यह कह सकता है कि यह चौकोर इमारत सारे जहानों के रब अल्लाह की शक्ल पर बनाई गई है? रहा हजरे-असवद, तो वह एक छोटा-सा पत्थर है जो काबा की चार दीवारी के एक कोने में आदमी के क़द के बराबर ऊँचाई पर लगा हुआ है। मुसलमान उसकी तरफ़ रुख़ करके सजदा नहीं करते। बल्कि काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) उस जगह से शुरू करके उसी जगह पर ख़त्म करते हैं। और हर तवाफ़ उसे चूमकर या उसकी ओर इशारा करके शुरू करते हैं। इसका आख़िर मूर्तिपूजा से क्या ताल्लुक़ है?
अब रही यह बात कि दुनिया भर के मुसलमान काबा ही की तरफ़ मुँह करके क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? तो इसका सीधा-सा जवाब यह है कि यह मर्कज़ियत (केन्द्रीयता) और तंज़ीम (संगठन) की ख़ातिर है। अगर सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मर्कज़ (केन्द्र), एक रुख़ तय न कर दिया गया होता तो हर नमाज़ के वक़्त अजीब अफ़रा-तफ़री पैदा होती रहती। अकेले-अकेले नमाज़ें पढ़ते समय एक मुसलमान का मुँह पश्चिम की तरफ़ होता तो दूसरे का पूरब की तरफ़, तीसरे का उत्तर की तरफ़ और चौथे का दक्षिण की तरफ़। और जब मुसलमान जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने खड़े होते तो हर मस्जिद में हर नमाज़ से पहले इस बात पर एक कानफ़्रेंस (सभा) होती कि आज किस तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। यही नहीं, बल्कि हर मस्जिद की तामीर के वक़्त हर मुहल्ले में यह झगड़ा उठ खड़ा होता कि मस्जिद का रुख़ किस तरफ़ हो। अल्लाह ने इन सारी आशंकाओं को एक क़िबला (दिशा) सुनिश्चित करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और क़िबला उसी जगह को बनाया जिसे फ़ितरी तौर पर केन्द्र होने की हैसियत हासिल होनी चाहिए थी। क्योंकि ख़ुदापरस्ती (ईश बन्दगी) का यह आन्दोलन इसी जगह से आरम्भ हुआ था और केवल एक ईश्वर की उपासना के लिए संसार में सबसे पहले इबादतगाह वही बनाई गई थी।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जि.61, संख्या न. 2, नवम्बर 1963 ई.)
नए दौर की रहनुमा ताक़त : इस्लाम या ईसाइयत?
सवाल
बीसवीं सदी के इस तहज़ीब व तरक़्क़ीयाफ़्ता दौर की रहनुमाई मज़हबी नुक़्त-ए-नज़र से इस्लाम कर सकता है या ईसाइयत? क्या इनसान को सेक्युलरिज़्म (धर्म निरपेक्षता) या दहरियत (नास्तिकता), रूहानी व माद्दी तरक़्की की ऊँचाइयाँ हासिल करा सकती है? ख़ास तौर से कम्युनिज़्म के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने और ख़त्म करने की सलाहियत किसमें है?
जवाब
यह सवाल कई सवालों का समूह है इसलिए इस सवाल के एक-एक हिस्से पर अलग-अलग बात होगी।
(1) जहाँ तक ईसाइयत का ताल्लुक़ है तो इस दौर की रहनुमाई से वह पहले ही अलग हो चुकी है। बल्कि हक़ीक़त में वह किसी दौर में भी इनसान की तहज़ीब और तमद्दुन से मुताल्लिक़ रहनुमाई नहीं कर सकी है। ईसाइयत से मुराद अगर हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की वे तालीमात हैं जो अब ईसाइयों के पास हैं, तो मौजूदा बाइबल को देखकर हर आदमी मालूम कर सकता है कि वह इनसान की तहज़ीब और तमद्दुन से मुताल्लिक़ क्या रहनुमाई और कितनी रहनुमाई करती है। इसमें कुछ सामान्य (Abstract) अख़्लाक़ी उसूलों के सिवा सिरे से कोई चीज़ मौजूद नहीं जिससे अपने समाज, व्यवसाय, सियासत, अदालत और क़ानून, के बारे में कोई हिदायत हासिल कर सकें। लेकिन अगर ईसाइयत से मुराद वह जीवन व्यवस्था है जो ईसाई पादरियों ने बनाई थी तो सब जानते हैं कि यूरोप में इल्म को ज़िन्दा करने की नई तहरीक के पैदा होने के बाद वह नाकाम हो गई और पश्चिमी क़ौमों ने उसके बाद जितनी कुछ भी माद्दी तरक़्क़ी की वह सब ईसाइयत की रहनुमाई से आज़ाद होकर की है। हालाँकि इस्लाम के ख़िलाफ़ ईसाइयों का तास्सुब और ईसाइयत के साथ जज़्बाती पक्षपात उनमें इसके बाद भी मौजूद रहा और अब भी है।
(2) जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है वह अपनी शुरुआत ही से तमद्दुन (सभ्यता) और तहज़ीब (संस्कृति) के मामले में न सिर्फ़ यह कि रहनुमाई करता रहा है बल्कि उसने ख़ुद अपना एक अलग तमद्दुन और तहज़ीब पैदा की है। इनसानी ज़िन्दगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसके बारे में क़ुरआन मजीद ने और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इनसान को हिदायत न दी हो और उन हिदायतों के मुताबिक़ अमली इदारे (व्यावहारिक संस्थाएँ) क़ायम न कर दिए हों। ये चीज़ें जिस तरह सातवीं सदी ईसवी में अमल के क़ाबिल थीं उसी तरह आज इक्कीसवीं सदी में भी अमल के क़ाबिल हैं और हज़ारों साल भी अगर अल्लाह ने चाहा तो अमल के क़ाबिल रहेंगी। ‘इस तरक़्क़ीयाफ़्ता दौर' में भी किसी ऐसी चीज़ की तरफ़ इशारा नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से इस्लाम आज न चल सकता हो या इनसान की रहनुमाई न कर सकता हो। जो आदमी इस मामले में इस्लाम को नाक़िस और अधूरा समझता हो, उसका काम है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताए जिसके मामले में इस्लाम उसकी रहनुमाई करने में बेबस नज़र आता हो।
(3) सेक्युलरिज़्म (धर्म निरपेक्षता) या नास्तिकता हक़ीक़त में न किसी रूहानी तरक़्क़ी में मददगार हैं और न ही दुनियावी तरक़्क़ी में। शिखर पर पहुँचने का सवाल ही क्या है? मैं यह समझता हूँ कि मौजूदा ज़माने में पश्चिमी लोगों ने जो तरक़्क़ी माद्दी हैसियत से की है वह सेक्युलरिज़्म या दुनियापरस्ती या नास्तिकता के ज़रिये से नहीं की, बल्कि इसके बावुजूद की है। मुख़्तसर तौर पर मेरी इस बात की दलील यह है कि इनसान कोई तरक़्क़ी इसके बग़ैर नहीं कर सकता कि वह अपने बुलंद मक़सद के लिए अपनी जान-माल की, अपने समय और मेहनतों की और अपने निजी फ़ायदों की क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो। लेकिन सेक्युलरिज़्म और नास्तिकता ऐसी कोई बुनियाद उपलब्ध करने में असमर्थ हैं जिस की बुनियाद पर इनसान यह क़ुरबानी देने को तैयार हो सके। इसी तरह कोई भी इनसानी तरक़्क़ी इज्तिमाई कोशिश के बग़ैर नहीं हो सकती, और इज्तिमाई (सामूहिक) कोशिश लाज़िमन इनसानों के बीच ऐसी दोस्ती चाहती है जिसमें एक-दूसरे के लिए प्यार और त्याग हो। लेकिन सेक्युलरिज़्म और नास्तिकता में मुहब्बत और त्याग के लिए कोई बुनियाद नहीं है। अब ये सारी चीज़ें पश्चिमी क़ौमों ने ईसाइयत से बग़ावत करने के बावुजूद उन मसीही अख़्लाक़ियात (नैतिक शिक्षाओं) ही से ली हैं जो उनकी सोसाइटी में रस्मी तौर पर बाक़ी रह गई थीं। इन चीज़ों को सेक्युलरिज़्म या नास्तिकता के हिसाब में लिखना ग़लत है। सेक्युलरिज़्म और नास्तिकता ने जो काम किया है वह यह कि पश्चिमी क़ौमों को ख़ुदा और आख़िरत से बेफ़िक्र करके ख़ालिस दुनियापरस्ती का आशिक़ और भौतिक आनन्दों एवं लाभों का इच्छुक बना दिया है, मगर उन क़ौमों ने इस मक़सद को हासिल करने के लिए जिन अख़्लाक़ी ख़ूबियों से काम लिया वे उनको सेक्युलरिज़्म या नास्तिकता से नहीं मिलीं, बल्कि उस मज़हब ही से मिलीं जिससे वे बग़ावत पर आमादा हो गए थे। इसलिए यह ख़याल करना सिरे से ग़लत है कि नास्तिकता या सेक्युलरिज़्म तरक़्क़ी की वजह हैं। वे तो इसके ख़िलाफ़ इनसान के अन्दर ख़ुदग़र्ज़ी, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कश-मकश और अपराध-पेशा के गुण पैदा करते हैं जो इनसान की तरक़्क़ी में मददगार नहीं बल्कि रुकावट हैं।
(4) कम्युनिज़्म के सैलाब को रोकने की सलाहियत किसी ऐसी ही जीवन व्यवस्था में हो सकती है जो इनसान की ज़िन्दगी के अमली मसलों को इससे बेहतर तरीक़े पर हल कर सके। इसके साथ ही इनसान को वह रूहानी सुकून भी पहुँचा सके जिसकी कमी कम्युनिज़्म में है। ऐसा निज़ाम अगर बन सकता है तो सिर्फ़ इस्लाम की बुनियाद पर बन सकता है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, अक्तूबर 1961 ई.)
इस्लाम और लोकतन्त्र
सवाल
जुमहूरियत (लोकतंत्र) को आजकल एक बेहतरीन निज़ाम (व्यवस्था) क़रार दिया जाता है। इस्लामी सियासी निज़ाम के बारे में भी यही ख़याल किया जाता है कि यह बहुत बड़ी हद तक जमहूरी (लोकतान्त्रिक) उसूलों पर आधारित है। मगर मेरी निगाह में जमहूरियत की कुछ ख़राबियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में यह मालूम करना चाहती हूँ कि इस्लाम उन्हें किस तरह दूर कर सकता है। वे ख़राबियाँ ये हैं—
(1) दूसरे सियासी निज़ामों (राजनीतिक व्यवस्थाओं) की तरह जमहूरियत में भी अमलन आख़िरकार हुकूमत जनता के हाथों से छिनकर और थोड़े से लोगों में केन्द्रित होकर दौलत के लिए जंगी सूरत अपना लेती है और Plutocracy या Obgacy की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इसका क्या हल मुमकिन है?
(2) आम लोगों के अलग-अलग और आपस में टकराने वाले फ़ायदों का एक साथ एक ही वक़्त ख़याल रखना नफ़्सियाती तौर पर एक बड़ा मुश्किल काम है। जमहूरियत इस अवामी ज़िम्मेदारी से किस शक्ल में अपना फ़र्ज़ अदा कर सकती है?
(3) आम लोगों की ज़्यादा तादाद जाहिल, सादालौह, बेहिस और शख़सियत-परस्त है और ख़ुदग़र्ज़ लोग उन्हें बराबर गुमराह करते रहते हैं, इन हालात में दूतावासी और लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए कामयाबी से काम करना बहुत ही कठिन है।
(4) जनता की ताईद से जो मजलिसें बनती हैं उनके सदस्यों की तादाद अच्छी-ख़ासी होती है और उनके बीच आपसी बहस व मशवरा और आख़िरी फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
आप हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि आपके ख़याल में इस्लाम अपने जमहूरी इदारों (लोकतान्त्रिक संस्थाओं) में इन ख़राबियों को राह पाने से कैसे रोकेगा?
जवाब
आपने लोकतन्त्र के बारे में जो तनक़ीद (आलोचना) की है उसकी सभी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इस मसले में आख़िरी राय क़ायम करने से पहले कुछ और बातों को निगाह में रखना ज़रूरी है।
पहला सवाल यह है कि इनसानी मामलों को चलाने के लिए उसूली तौर पर कौन-सा तरीक़ा सही है? क्या यह कि वे मामले जिन लोगों से ताल्लुक़ रखतें हैं उनकी मर्ज़ी से चलानेवाले चुने जाएँ और वे उनके मशविरे और रज़ामन्दी से मामलात चलाएँ और जब तक उनका भरोसा सरबराहकारों (चलानेवालों) को हासिल रहे उसी वक़्त तक वे ज़िम्मेदार रहें? या यह कि कोई आदमी या गरोह ख़ुद इन्तिज़ाम चलानेवाला बन बैठे और अपनी मर्ज़ी से मामलात चलाए और उसके तक़र्रुर (नियुक्ति) और बर्ख़ास्तगी (निकालने) और कारपरदाज़ी (काम करने) में से किसी चीज़ में भी उन लोगों की मर्ज़ी व राय का कोई दख़ल न हो जिनके मामलात वह चला रहा हो? अगर इनमें से पहली सूरत ही सही और इंसाफ़ पर क़ायम है तो हमारे लिए दूसरी सूरत की तरफ़ जाने का रास्ता पहले ही क़दम पर बन्द होना चाहिए और सारी बहस इसपर होनी चाहिए कि पहली सूरत को अमल में लाने का ज़्यादा-से-ज़्यादा बेहतर तरीक़ा क्या है।
दूसरी बात जो निगाह में रहनी चाहिए वह यह है कि लोकतन्त्र के उसूल को अमल में लाने की जो बेशुमार शक्लें अलग-अलग ज़मानों में अपनाई गई हैं या तजवीज़ (प्रस्तावित) की गई हैं, उनकी तफ़सीलात से अगर उन्हें सिर्फ़ इस लिहाज़ से जाँचा और परखा जाए कि जमहूरियत के उसूल और मक़सद को पूरा करने में वे कहाँ तक सफल होती हैं, तो कमी के बुनियादी असबाब (कारण) सिर्फ़ तीन ही पाए जाते हैं—
पहला यह कि 'जमहूर' (जनता) को मुख़्तारे-मुतलक़ (सर्वाधिकारी) और हाकिमे-मुतलक़ (Sovereign) मान लिया गया और इस बुनियाद पर लोकतन्त्र को मुत्लक़ुलइनान यानी निरंकुश बनाने की कोशिश की गई। हालाँकि जब बजाए ख़ुद इनसान ही इस कायनात में मुख़्तारे-मुतलक़ नहीं है तो इनसान पर आधारित कोई लोकतन्त्र शासन चलाने योग्य कैसे हो सकता है? इसी आधार पर निरंकुश लोकतन्त्र स्थापित करने की कोशिश आख़िरकार जिस चीज़ पर ख़त्म होती रही है वह जनता पर कुछ लोगों की अमली बादशाहत है। इस्लाम पहले ही क़दम पर इसका सही इलाज कर देता है। वह लोकतन्त्र को ऐसे बुनियादी क़ानून का पाबन्द बनाता है जो कायनात के अस्ल हाकिम (Sovereign) ने मुक़र्रर किए हैं। इस क़ानून की पाबन्दी प्रजा और उसके शासकों को अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। इस कारण वह निरंकुशता सिरे से पैदा ही नहीं होने पाती जो आख़िरकार लोकतन्त्र की असफलता का मूल कारण बनती है।
दूसरा यह कि कोई लोकतन्त्र उस वक़्त तक नहीं चल सकता जब तक जनता में उसका बोझ सहने के लायक़ शऊर और मुनासिब अख़लाक़ न हों। इस्लाम में इसी लिए आम मुसलमानों की फ़रदन-फ़रदन (व्यक्तिगत रूप से) तालीम और अख़लाक़ी (नैतिक) तरबियत पर ज़ोर दिया गया है। उसकी माँग है कि एक-एक मुसलमान में ईमान, एहसासे-ज़िम्मेदारी और इस्लाम के बुनियादी हुक्मों पर अमल करने का और उनकी पाबन्दी का इरादा पैदा हो। यह चीज़ जितनी कम होगी लोकतन्त्र की कामयाबी के इमकान उतने ही कम होंगे, और यह जितनी ज़्यादा होगी इमकान उतने ही ज़्यादा होंगे।
तीसरा यह कि लोकतन्त्र के कामयाबी के साथ चलने का दारोमदार एक बेदार, मज़बूत जनता की राय (मत) पर है और जनता की इस तरह की राय उसी वक़्त पैदा होती है जब समाज अच्छे लोगों पर बना हो। इन लोगों को नेक बुनियादों पर एक सामूहिक व्यवस्था में जोड़ दिया गया हो और उस सामूहिक व्यवस्था में इतनी ताक़त मौजूद हो कि बुराई और बुराई करने वाले उसमें न फल-फूल सकें और नेकी और नेक लोग ही उसमें उभर सकें। इस्लाम ने इसके लिए हमको तमाम ज़रूरी हिदायतें दे दी हैं।
अगर ऊपर लिखी तीनों चीज़ें मिल जाएँ तो जमहूरियत (लोकतंत्र) पर अमल दरामद की मशीनरी चाहे किसी तरह की बनाई जाए वह कामयाबी के साथ चल सकती है। उस मशीनरी में किसी जगह कोई ख़राबी महसूस हो तो उसका सुधार करके बेहतर मशीनरी भी बनाई जा सकती है। इसके बाद सुधार और तरक़्क़ी के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि जमहूरियत के तजरबे का मौक़ा मिले। तजरबों से धीरे-धीरे एक नाक़िस (ख़राब) मशीनरी बेहतर-से-बेहतर बनती चली जाएगी।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जून, 1968 ई.)
गुनाहगार मोमिन और 'नेको-कार' काफ़िर का फ़र्क़
सवाल
आजकल एफ़. एस. सी. की छात्रा, एक बहुत ही ज़हीन ईसाई लड़की, मेरे पास अंग्रेज़ी पढ़ने आती है। वह तक़रीबन रोज़ाना मुझसे मज़हबी बातों पर विचारों का आदान-प्रदान करती है। मैं भी इस मौक़े को अच्छा समझते हुए उसे दीने-इस्लाम की तालीमात से रूशनास (परिचित) कराने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दीने-इस्लाम के बारे में उसकी बहुत-सी ग़लतफ़हमियों को दूर कर दिया है।
लेकिन एक दिन उसने मेरे सामने एक सवाल ऐसा रख दिया जिसका जवाब मुझे न सूझ सका। इसके बाद मैंने आपकी किताबों से भी खोजबीन की मगर अब तक कोई मुत्मइन कर देनेवाले इशारे वहाँ से नहीं मिल सके।
मेरी ईसाई छात्रा कहने लगी कि मैंने मैट्रिक में इस्लामियात के कोर्स में एक हदीस पढ़ी थी जिसमें कहा गया है कि मुसलमान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार हो वह कुछ अरसे दोज़ख़ (जहन्नम) में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतकर आख़िरकार ज़रूर जन्नत में चला जाएगा। मगर काफ़िर हमेशा-हमेशा के लिए दोज़ख़ में रहेंगे। फिर वह कहने लगी कि आप हमें भी काफ़िर समझते हैं। कोई ईसाई चाहे वह कितना ही नेकोकार (सत्कर्मी) हो मुसलमानों के अक़ीदे (आस्था) के मुताबिक़ दोज़ख़ ही में जाएगा। आख़िर इसकी क्या वजह है?
जवाब
आप अपनी शागिर्द को पहले यह बात समझाएँ कि गुनाहगार मोमिन और नेकोकार काफ़िर के बीच फ़र्क़ की बुनियाद क्या है। मोमिन अल्लाह की फ़रमाँबरदारी क़बूल करके उसके वफ़ादार बन्दों में शामिल हो जाता है। इसके बाद अपनी अख़लाक़ी कमज़ोरियों की वजह से वह किसी जुर्म या जुर्मों को कर बैठता है। इसके प्रतिकूल काफ़िर अस्ल में बाग़ी होता है और आपके कहने के मुताबिक़ अगर वह नेकोकार हो भी तो उसके मानी सिर्फ़ ये हैं कि उसने बग़ावत के जुर्म पर किसी और जुर्म का इज़ाफ़ा (बढ़ोत्तरी) नहीं किया। अब यह ज़ाहिर है कि जो आदमी बाग़ी नहीं है और सिर्फ़ मुजरिम है उसे सिर्फ़ जुर्म की हद तक सज़ा दी जाएगी, बग़ावत की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। क्योंकि जुर्म करने की वजह से कोई शख़्स वफ़ादारी के दायरे से ख़ारिज नहीं हो जाता। लेकिन बग़ावत अपने-आप में सबसे बड़ा जुर्म है, इसके साथ ही अगर कोई शख़्स दूसरे जराइम (अपराधों) का इज़ाफ़ा न भी करता हो तो उसे वह हैसियत किसी तरह नहीं दी जा सकती जो वफ़ादार को दी जाती है। वह बग़ावत की सज़ा हर हाल में पाकर रहेगा। चाहे वह इसके अलावा कोई और जुर्म न करे। लेकिन अगर वह बाग़ी होने के साथ-साथ कुछ और जुर्म भी करता है तो उसे बग़ावत की सज़ा के साथ-साथ उन दूसरे जुर्मों की सज़ा भी दी जाएगी।
इस उसूली बात को जब वे समझ लें तो उनको बताइए कि अल्लाह की वफ़ादार और फ़रमाँबरदार रैयत (प्रजा) में सिर्फ़ वे लोग शामिल होते हैं जो अल्लाह को एक मानने के साथ किसी को उसके साथ शरीक किए बग़ैर, और अल्लाह के सब पैग़म्बरों को बिना किसी भेदभाव के और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को किसी का इनकार किए बग़ैर मानते हों और आख़िरत (परलोक) की जवाबदेही को भी तसलीम करते हों। इनमें से जिस चीज़ को भी आदमी न मानेगा वह बाग़ी होगा और उसे ख़ुदा की वफ़ादार जनता में शुमार न किया जा सकेगा। अब मिसाल के तौर पर रसूलों और किताबों ही के मामले को ले लीजिए। हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) और उनकी इंजील को जब यहूदियों ने न माना तो वे सब बाग़ी हो गए। हालाँकि ईसा (अलैहिस्सलाम) से पहले के नबियों और उनकी लाई हुई किताबों को वे मानते थे। इसी तरह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आमद (आगमन) से पहले तक हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की पैरवी करनेवाले अल्लाह की वफ़ादार रैयत थे। लेकिन जब उन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और क़ुरआन मजीद को मानने से इनकार कर दिया तो वे भी बाग़ी हो गए। ईसा (अलैहिस्सलाम) इंजील और पहले के नबियों और उनकी किताबों को मानने के बावजूद वे अल्लाह की वफ़ादार और आज्ञाकारी रैयत (प्रजा) में शामिल नहीं हो सकते।
यह बात भी जब वे समझ लें तो उन्हें बताइए कि अल्लाह ने अपनी जन्नत अपने बाग़ियों के लिए नहीं बनाई है बल्कि अपने वफ़ादार और फ़रमाँबरदार रैयत के लिए बनाई है। इस वफ़ादार रैयत में से अगर कोई आदमी ऐसा जुर्म जो माफ़ करने के लायक़ न हो करता है या इस तरह के बहुत-से जुर्मों को कर बैठता है तो उसे उसके जुर्मों के मुताबिक़ सज़ा दी जाएगी। और जब वह अपनी सज़ा भुगत लेगा तो जन्नत में दाख़िल कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने बग़ावत का जुर्म किया है वह किसी तरह जन्नत में नहीं जा सकता। उसकी जगह हर हाल में दोज़ख़ है। दूसरे किसी जुर्म का करनेवाला न भी हो तो बग़ावत ख़ुद एक इतना बड़ा जुर्म है जिसके साथ कोई नेकी भी उसे जन्नत में नहीं पहुँचा सकती। (तर्जमानुल-क़ुरआन, अगस्त 1975 ई०)
हक़ की तलाश का सही तरीक़ा
सवाल
अगर एक आदमी हक़ की तलाश में है और वह दिल से उसकी कोशिश भी करता है लेकिन उसे काफ़ी दौड़-धूप के बाद भी वह नहीं मिलता तो क्या वह बेचारा हौसला हार नहीं बैठेगा? इसकी मिसाल यूँ है कि एक आदमी घनघोर अंधेरे में इस ग़रज़ से सफ़र करता है कि कहीं रौशनी का चिराग़ उसे मिले। लेकिन सफ़र करते-करते रौशनी का निशान तक उसे नहीं मिलता। आख़िर को बेचारा थक-हारकर बैठ जाता है और यह समझ लेता है कि रौशनी सिरे से है ही नहीं, अगर कुछ है तो बस घुप अंधेरा।
मौलाना मुहतरम, आप कहेंगे कि मैंने यह एक सिर्फ़ फ़र्ज़ी मिसाल पेश की है। मैं इनसानी ज़िन्दगी में अमली मिसाल पेश करता हूँ। दो आदमी हैं जो शऊरी (अक़्ली) तौर पर और रस्मी तौर पर मुसलमान हैं। शुरू-शुरू में दोनों चहारदीवारियों के अन्दर बन्द होते हैं जिनमें से हर एक चहारदीवारी ज़िन्दगी में मुसीबतों, तकलीफ़ों और नाकामियों की चहारदीवारी है। एक आदमी पहले घेरे से बाहर निकल आता है और समझ लेता है कि अब एक ही घेरा उसके लिए बाक़ी है जिससे निकलकर वह आज़ाद हो जाएगा। इस तरह उसका हौसला बढ़ जाता है और जब वह दूसरी चहारदीवारी से भी बाहर निकल आता है तो आज़ाद हो जाता है। यह तजरबा उसे मुत्मइन कर देता है और वह ऐसी ताक़त का क़ायल हो जाता है जो मुसीबत में फँसे लोगों की पुकार को सुनती है और मदद करती है। मगर दूसरा आदमी एक चहारदीवारी से निकलता है तो दूसरी चहारदीवारी और दूसरी से निकलता है तो तीसरी चहारदीवारी उसे घेर लेती है। यहाँ तक कि एक के बाद एक चहारदीवारी उसे घेरती चली जाती है। यह मुसलसल चक्कर उसे बिल्कुल मायूस कर देता है और वह किसी ऐसी ताक़त से जो मुसीबत में काम आए पूरे तौर पर नाउम्मीद हो जाता है। क्योंकि बेचारा बार-बार चिल्लाता है कि "अल्लाह की मदद कब आएगी?" और कभी बेचारे को "जान लो अल्लाह की मदद क़रीब है" की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यह आदमी इसलिए नाउम्मीद हो गया है कि बेचारे की बेशतर (अधिकांश) ख़ाहिशों में से एक भी पूरी नहीं हुई और बीस तकलीफ़ों में से एक भी दूर नहीं होती। अगर कोई एक ख़ाहिश भी पूरी हो जाती या एक तकलीफ़ भी दूर हो जाती तो वह इस बात से पूरे तौर पर मायूस न होता कि ऊपर कोई सबसे बड़ी ताक़त दुआएँ सुनने और हाजतें पूरी करने वाली मौजूद है।
जवाब
आपने अपने सवाल के शुरू में जो बात लिखी है उसका जवाब यह है कि हक़ की तलाश एक बुनियादी ख़ूबी है जो हक़ पाने के लिए पहली शर्त की हैसियत रखती है। लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि हक़ की तलाश दिल से हो, बिना तास्सुब और बिना भेदभाव के हो और दानिशमन्दी (विवेक) के साथ हो। यानी आदमी इस तलाश के दौरान में हक़ और बातिल के बीच तमीज़ करता रहे और जो चीज़ बातिल नज़र आए उसे छोड़कर हक़ को क़बूल करता चला जाए। इस सूरत में यह इमकान न होने के बराबर है कि आदमी को घुप अँधेरे के सिवा कुछ न मिले।
सवाल के दूसरे हिस्से में आपने जो मिसाल पेश की है, उससे मालूम होता है कि हक़ की खोज हक़ को पाने के लिए नहीं बल्कि इस ग़रज़ से कर रहे हैं कि आप मुसीबतों, तकलीफ़ों और नाकामियों की चहारदीवारी से निकल जाएँ और आपको "अल्लाह की मदद कब आएगी" के जवाब में "जान लो अल्लाह की मदद क़रीब है" की आवाज़ न सिर्फ़ यह कि सुनाई देने लगे बल्कि वह जवाब देने वाली हस्ती आपकी मुसीबतों, आफ़तों, तकलीफ़ों और नाकामियों का इलाज भी कर दे।
मेरे ख़याल में हक़ की खोज के लिए यह शुरुआती क़दम ही सिरे से ग़लत है जिसकी वजह से आपको मायूसी का सामना करना पड़ा। हक़ की तलाश का सही रास्ता जो आपको अपनाना चाहिए वह यह है कि:—
सबसे पहले मुताला (अध्ययन) और चिन्तन-मनन से यह पूरी तहक़ीक़ करें कि क्या इस कायनात का यह निज़ाम बिना ख़ुदा के है? या बहुत-से बाइख़्तियार (अधिकार प्राप्त) ख़ुदाओं के बनाने से बना है और वे सब इसका निज़ाम (व्यवस्था) चला रहे हैं। या इसका एक ही ख़ालिक़ (बनानेवाला), मालिक, हाकिम और इन्तिज़ाम करनेवाला है?
इसके बाद आप इस कायनात को समझने की कोशिश करें और यह खोजबीन करें कि क्या यह अज़ाब का घर है? या ऐशो-आराम का घर? या इम्तिहान की जगह है जिसमें मज़े और तकलीफ़, सुख और दुख, कामयाबी और नाकामी, हर चीज़ आज़माइश के लिए है?
फिर आप इस दुनिया में इनसान की हैसियत को समझने की कोशिश करें कि क्या वह यहाँ बिल्कुल आज़ाद और पूरा इख़्तियार पाया हुआ है और कोई सबसे बड़ी ताक़त उसकी क़िस्मत पर असरअंदाज़ होनेवाली नहीं है और किसी सबसे बड़ी ताक़त के सामने वह जवाबदेह (उत्तरदायी) नहीं है? या ज़मीन और आसमान में बहुत-से ख़ुदा उसकी क़िस्मत के मालिक हैं? या एक ही ख़ुदा उसका और सारी दुनिया का पैदा करनेवाला और हाकिम है और वह हर ताक़त से बढ़कर है। हमारी लगाई हुई शर्तों का पाबन्द नहीं है। और वह हमारे आगे जवाबदेह नहीं, बल्कि हम उसके आगे जवाबदेह हैं। और वह यहाँ अच्छी या बुरी सब तरह की हालतों में रखकर हमारा इम्तिहान ले रहा है, जिसका नतीजा इस दुनिया में नहीं बल्कि आख़िरत में निकलेगा?
इन तीन सवालों में से अगर आपकी तहक़ीक़ (खोजबीन) हर एक का जवाब पहली या दूसरी शक्ल में दे तो आपको मायूसी की हालत से निकलकर उम्मीद का रास्ता पाने की कोई सूरत बताना मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता अगर आपकी तहक़ीक़ हर सवाल का जवाब तीसरी शक्ल में दे तो यही जवाब आपको दिली सुकून और इतमीनान की मंज़िल तक पहुँचा सकता है, शर्त यह है कि आप और ज़्यादा चिन्तन-मनन करके उसके मंतिक़ी नुक़सानात (Logical Implications) को अच्छी तरह समझते चले जाएँ।
जब एक ख़ुदा जिसका कोई शरीक भी नहीं है सारी कायनात के इन्तिज़ाम को चला रहा है तो कायनात की आबादी के अनगिनत लोगों में से किसी शख़्स का यह चाहना ही सिरे से ग़लत है कि ख़ुदा की सारी ख़ुदाई सिर्फ़ उसके ही फ़ायदे के लिए काम करे।
जब यह दुनिया एक इम्तिहान की जगह है तो इसमें पेश आनेवाली हर ख़ुशी और ग़म, हर सुख और दुख, हर कामयाबी और नाकामी अस्ल में इनसान की आज़माइश के लिए है। यह बात जिस आदमी को भी समझ में आजाएगी वह न किसी अच्छी हालत पर इतराएगा और न किसी बुरी हालत पर दिल-शिकस्ता (ग़मगीन) होगा। बल्कि हर हालत में उसकी कोशिश यह होगी कि ख़ुदा के इम्तिहान में कामयाब हो। दुनिया के मौजूदा निज़ाम की इस हक़ीक़त को जान लेने के बाद आदमी यहाँ ऐसी ग़लत तमन्नाएँ दिल में पालेगा ही नहीं कि इस ज़िन्दगी में उसे ख़ालिस ऐश, बेलाग लज़्ज़त, आराम ही आराम और हमेशा रहनेवाली कामयाबी नसीब हो और कभी उसे मुसीबत, दुख-तकलीफ़ और नाकामी से सामना ही न पड़े। क्योंकि यह दुनिया न ऐश का घर है और न अज़ाब का घर कि यहाँ सिर्फ़ मज़े या सिर्फ़ दुख, या सिर्फ़ राहत, या सिर्फ़ तकलीफ़, या महज़ कामयाबी, या महज़ नाकामी कहीं पाई जा सके।
इसी तरह जब तीसरे सवाल का जवाब आप खोजबीन से यह पा लें कि एक ख़ुदा जो सबका पैदा करनेवाला और हाकिम है और हम सब उसके महकूम (शासित) और ग़ुलाम हैं और यह कि वह सबसे बढ़कर ताक़तवाला और हर क़ुदरत वाला है और हम सब उसके बन्दे होते हुए उसे अपनी शर्तों का पाबन्द नहीं बना सकते, और यह कि वह हमारे सामने नहीं बल्कि हम उसके सामने जवाबदेह हैं, तो आपका दिमाग़ कभी ख़ुदा से ग़लत उम्मीदें नहीं लगाएगा कि हम ख़ुद जिस हालत में रहना चाहते हैं वह हमें उसी हालत में रखे और हम जो दरख़्वास्त भी उससे करें वह ज़रूर उसी शक्ल में उसे पूरा करे जो हमने पसन्द की है, और हमपर कोई तकलीफ़ या मुसीबत अगर आ ही जाए तो हमारी माँग पर वह उसे तुरन्त दूर कर दे।
मुख़्तसर बात यह है कि सही पहचान और समझ का फल इतमिनान है जो हर अच्छे या बुरे हाल में बराबर बना रहता है, और पहचान और समझ के न होने का नतीजा हर हाल में बेचैनी, परेशानी और मायूसी है चाहे आरज़ी तौर पर इनसान अपनी कामयाबियों से ग़लतफ़हमी में पड़कर कितना ही मगन हो जाए। आप मायूसी से निकलना चाहते हैं तो पहले हक़ीक़त की पहचान और समझ हासिल करने की फ़िक्र करें, वरना कोई चीज़ भी आपको घुप अँधेरे से बाहर न निकाल सकेगी। (तर्जमानुल-क़ुरआन, अगस्त 1975)
हराम की गई औरतों (मुहर्रमात) के हराम होने की वजहें
सवाल
कुछ दिनों से दोस्तों के बीच हराम की गई औरतों के सिलसिले में एक मसला बहस का विषय बना हुआ है जिसे मैं नीचे लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसपर रौशनी डालने की मेहरबानी फ़रमाएँगे।
शादी-ब्याह के सिलसिले में एक औरत और दूसरी औरत में क्यों भेद-भाव किया गया है कि कुछ के साथ निकाह किया जा सकता है और कुछ औरतें हराम की फ़ेहरिस्त (सूची) में आती हैं, उनसे निकाह नहीं किया जा सकता? हालाँकि शुरू के इनसानी समाज में ऐसी कोई पाबंदी नज़र नहीं आती है जैसा कि हाबील और क़ाबील के क़िस्से से मालूम होता है। इसमें क्या हिकमत है? क्या इस क़िस्म की शादियाँ हयातयाती (जैविक) बिगाड़ की वजह भी बन सकती हैं? उम्मीद है कि आप इसका जवाब (माहाना मैग़ज़ीन) तर्जमानुल-क़ुरआन में देगें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँच सके।
जवाब
हराम की गई औरतों की सूची में जिन औरतों को शामिल किया गया है उनके हराम होने की अस्ल वजह हयातयाती हक़ीक़तें नहीं हैं, बल्कि अख़्लाक़ी और सामाजिक सच्चाइयाँ हैं। आप ख़ुद ग़ौर करें कि जिस माँ की कामुक भावनाएँ भी अपने बेटे के साथ हो सकती हों, क्या वह उन पाकीज़ा जज़्बात के साथ बेटे को पाल सकती है जो माँ और बेटे के ताल्लुक़ात में होने चाहिएँ?
क्या बेटा भी होश सँभालने के बाद माँ के साथ वह मासूमियत भरी बेतकल्लुफ़ी बरत सकता है जो माँ और बेटे के बीच अब होती है? और क्या एक घर में बाप और बेटे के बीच रक़ाबत (दुश्मनी) और हसद की भावनाएँ पैदा न हो जाएँगी अगर माँ और बेटे के बीच हुरमत (हराम होने) की मज़बूत दीवार खड़ी न हो?
ऐसा ही मामला बहन और भाई का भी है। अगर हमेशा की हुरमत उनके बीच क़ायम न होती तो क्या यह मुमकिन था कि भाई-बहन एक दूसरे के साथ वासनात्मक ताल्लुक़ात से पाक मुहब्बत और कामुक शंकाओं से ऊपर उठकर बेतकल्लुफ़ी बरत सकते? क्या इस सूरत में भी यह मुमकिन होता कि माँ-बाप अपने बेटों को जवानी के क़रीब पहुँचने पर एक-दूसरे से दूर रखने की कोशिश न करते? और क्या कोई व्यक्ति किसी लड़की से शादी करते वक़्त यह इत्मीनान कर सकता था कि वह अपने भाइयों से बची हुई होगी?
फिर आख़िर ससुर और बहू के बीच, और सास और दामाद के बीच हमेशा हराम रहने की दीवारें न खड़ी कर दी जातीं तो किस तरह मुमकिन था कि बाप-बेटे और माँ-बेटियाँ एक-दूसरे के साथ रक़ीबाना और जलन जैसी कशमकश में पड़ जाने और एक-दूसरे को सन्देह की नज़र से देखने से बच जाएँ?
इस पहलू पर अगर आप ग़ौर करें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शरीअत ने किन अहम (महत्वपूर्ण) नैतिक और सामाजिक मस्लहतों की बुनियाद पर उन तमाम मर्दों और औरतों को एक-दूसरे के लिए हराम कर दिया है जिनके बीच एक घर, एक ख़ानदान और एक सामाजिक घेरे के अन्दर क़रीबतरीन और बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ फ़ितरी तौर पर होते हैं और सामाजिक ज़रूरतों के लिहाज़ से होने चाहिएँ। बेटे और बेटियाँ पल ही नहीं सकतीं अगर माँ और बाप दोनों इस तरफ़ से बिल्कुल मुतमइन न हों कि उनमें से किसी का भी कोई शहवानी ताल्लुक़ (Sexual Relation) अपनी औलाद के साथ नहीं है। एक ही घर में लड़कियों और लड़कों का पलना ग़ैर मुमकिन हो जाए अगर बहन के मामले में भाइयों के बीच शहवानी रक़ाबत पैदा होने का दरवाज़ा पूरी तरह बन्द न हो। ख़ालाएँ (मौसी) और फूफियाँ और चचा और मामू अगर शंका से मुक्त न कर दिए जाएँ तो बहन अपनी औलाद को अपने भाई-बहनों से और भाई अपनी औलाद को अपने भाई-बहनों से बचाने की फ़िक्र में लग जाएँ। (तर्जमानुल-क़ुरआन, सितम्बर 1951 ई.)
बहुविवाह पर पाबन्दी
सवाल
मैं आपसे एक मसले के बारे में जानना चाहता हूँ, वह यह कि अगर इस्लामी स्टेट में औरतों की तादाद मर्दों से कम हो तो क्या हुकूमत इस बुनियाद पर बहुविवाह पर पाबन्दी लगा सकती है? इस सवाल की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की है कि मेरा अन्दाज़ा यह है कि क़ुरआन मजीद ने जहाँ बहुविवाह या एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त दी है वहाँ हंगामी सूरते-हाल सामने थी। उस ज़माने में सालहा-साल के मुसलसल जिहाद के बाद बहुत-सी औरतें बेवा हो गई थीं और बच्चे बेसहारा और यतीम रह गए थे। इस सूरते-हाल से निबटने के लिए यह इजाज़त दी गई थी, ताकि बेवाओं और यतीम बच्चों को सोसाइटी में जगह मिल सके और उनके पालन-पोषण की बेहतर सूरत पैदा हो सके।
जवाब
आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि किसी समाज में औरतों की तादाद का मर्दों से इतना कम होना कि इससे समाजी मसला पैदा हो जाए एक कभी-कभार की बात है। आमतौर पर तादाद मर्दों ही की कम होती रहती है। औरतों की तादाद कम होने के कारण वे नहीं हैं जो मर्दों की तादाद कम होने के हैं। औरतें अगर कम होंगी तो इस वजह से कि बच्चियों की पैदाइश ही बच्चों से कम हो। ऐसा होना अव्वल तो बहुत ही कम है, और अगर हो भी तो औरतों की इतनी कम पैदाइश नहीं होती कि इसकी वजह से एक सामाजिक मसला पैदा हो और उसे हल करने के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत पेश आए। बेवा और तलाक़शुदा औरतों की शादी के रिवाज से यह मसला ख़ुद ही हल हो जाता है।
रही दूसरी बात जो आपने लिखी है वह क़ुरआन के सही मुताले की बुनियाद पर नहीं है। इस्लाम के किसी दौर में भी एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना मना नहीं था। कोई ख़ास वक़्त भी ऐसा नहीं आया कि इस रोक को किसी मसलिहत की बुनियाद पर हटा करके यह काम जायज़ किया गया हो। अस्ल में कई बीवियाँ रखना (बहुविवाह) हर ज़माने में तमाम नबियों की शरीअतों (विधानों) में जायज़ रहा है और जाहिली अरब-समाज में भी यह जाइज़ और चलन में था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की रिसालत के बाद सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) भी और ख़ुद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी इसपर अमल कर रहे थे। क़ुरआन मजीद में कोई आयत ऐसी नहीं है जिससे यह अंदेशा किया जा सकता हो कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले कई बीवियाँ रखना नाजाइज़ था और इस आयत ने आकर उसे जाइज़ किया। आपके इल्म में ऐसी कोई आयत हो तो उसका हवाला दें।
सवाल
आप मुझे माफ़ करें अगर मैं यह अर्ज़ करूँ कि आपके जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मेरी गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी थी कि अगर किसी समाज में औरतों की तादाद मर्दों से कम हो जाए तो क्या इस सूरत में हुकूमत को यह हक़ हासिल है कि वह एक से ज़्यादा शादियों पर पाबन्दी लगा सके? आपने फ़रमाया कि ऐसा बहुत ही कम हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल भी इसी बहुत ही कम और कभी-कमार होने की सूरत से ताल्लुक़ रखता है। आपको मालूम होगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में (जनगणना के अनुसार) औरतें मर्दों के मुक़ाबले में कम हैं। अब क्या हुकूमत कोई ऐसा क़ानून बना सकती है कि जब तक यह हालत बनी रहे एक से ज़्यादा शादियों पर पाबन्दी लग जाए?
मैनें अर्ज़ यह किया था कि कई बीवियाँ रखने की इज़ाज़त का मतलब शायद यह है कि उस ज़माने में जब प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस्लाम की दावत देने में बिज़ी थे तो लगातार वर्षों जिहाद की वजह से बेवा औरतों और यतीम बच्चों का मसला हल करना पड़ा और उसका हल यह निकाला गया कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दे दी जाए। जिस जगह यह इजाज़त दी गई है उससे पहले जिहाद व क़िताल (जंगों) ही का बयान आया है। इस तरह मैंने (ग़लत या सही) यह नतीजा निकाला है कि यह इजाज़त ख़ास हालतों के लिए ही हो सकती है। अगर यह मतलब निकालना ग़लत भी है और जैसा कि आपने फ़रमाया है कि यह क़ुरआन के सही मुताले (अध्ययन) की बुनियाद पर नहीं है तो इससे हटकर भी यही कुछ सोचा जा सकता है कि दो-दो, तीन-तीन और चार-चार निकाह उसी सूरत में किए जा सकते हैं, जबकि समाज में औरतों की तादाद मर्दों के मुक़ाबले में ज़्यादा हो। अगर उनकी तादाद मर्दों के मुक़ाबले में ज़्यादा न हो या मर्दों के बराबर हो तो इस इज़ाज़त से फ़ायदा उठाने की क्या ज़रूरत है?
जवाब
पाकिस्तान की जनगणना में औरतों की तादाद का मर्दों से कम पाया जाना इस बात की दलील नहीं है कि हक़ीक़त में हमारे यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से कम है, बल्कि इसमें हमारे यहाँ के रीति-रिवाजों को बड़ा दख़ल है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की औरतों का नाम दर्ज कराने से परहेज़ करते हैं। फिर भी अगर करोड़ों की आबादी में कुछ हज़ार या लाख का फ़र्क़ हो भी तो इससे कोई ऐसा समाजी मसला पैदा नहीं होता जिसके लिए एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर पाबन्दी लगाने की ज़रूरत पेश आए। यह मसला बेवा और तलाक़-शुदा औरतों के दोबारा निकाह कराने से हल हो जाता है। मान भी लिया जाए अगर कोई बहुत ही ग़ैर-मामूली कमी हो ही जाए तो वक़्ती तौर पर कुछ मुद्दत के लिए पाबन्दी लगा देना भी जाइज़ हो सकता है, शर्त यह है कि इस पाबन्दी का अस्ल सबब यही मसला हो। लेकिन इस बात को छिपाने की आख़िर क्या ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर पाबन्दी लगाने की ज़रूरत अस्ल में इस बुनियाद पर महसूस नहीं की गई है बल्कि इसका अस्ल मुहर्रिक (प्रेरक) पश्चिमी सोच है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना अपने आप में एक बुराई है और क़ानून के मुताबिक़ एक ही बीवी रखने का रिवाज देना मक़सद है। यह मुहर्रिक (प्रेरक) हमारे नज़दीक बहुत ही क़ाबिले-एतिराज़ है और इसकी जड़ काटना हम ज़रूरी समझते हैं।
मैने पहले भी लिखा था और अब फिर दोहरा रहा हूँ कि क़ुरआन मजीद में कोई आयत कई बीवियाँ रखने की इजाज़त देने के लिए नहीं आई है। एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने का रिवाज पहले से ही जाइज़ चला आ रहा था और सूरा निसा की आयत नम्बर तीन के नाज़िल होने से पहले ख़ुद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घर में तीन पाक बीवियाँ मौजूद थीं। सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी बहुत-से ऐसे थे जिनके यहाँ एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं। सूरा निसा की यह आयत इस जाइज़ काम की इजाज़त देने के लिए नहीं आई थी बल्कि इस गरज़ के लिए आई थी कि उहुद की जंग में बहुत-से सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के शहीद हो जाने और बहुत-से बच्चों के यतीम हो जाने से फ़ौरी तौर पर जो सामाजिक मसला पैदा हो गया था उसके हल करने की सूरत मुसलमानों को यह बताई गई कि अगर तुम यतीमों के साथ वैसे इनसाफ़ नहीं कर सकते तो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार औरतों से निकाह करके उन यतीमों को अपनी सरपरस्ती में ले लो। इसका यह मतलब नहीं है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना सिर्फ़ ऐसे ही मसले पैदा होने की सूरत में जाइज़ है। आख़िर तेरह-चौदह सौ वर्षों से हमारे समाज में यह तरीक़ा चला आ रहा है। इससे पहले कब यह सवाल पैदा हुआ था कि एक से ज़्यादा बीवियों के रखने की इजाज़त ख़ास हालात पैदा होने की शर्त के साथ है? इस तरह की सोच हमारे यहाँ पश्चिम के ग़लबे से पैदा हुई है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, मई 1963 ई.)
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कई शादियों में क्या हिकमत थी?
सवाल
मैं आजकल अमेरिका में रह रहा हूँ। यहाँ ईसाइयों से मज़हबी मामलों पर विचार-विमर्श होता रहता है। ये लोग और ख़ास तौर पर उनके मज़हबी रहनुमा कई शादियाँ करने के मसले पर बहुत उलझते हैं। यह चीज़ किसी तरह उनकी समझ में नहीं आती। इस सिलसिले में वे हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नौ शादियों पर एतिराज़ उठाते हैं और कहते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से बहुत छोटी उम्र में शादी की जिसकी ज़रूरत समझ से बाहर है।
मैं और मेरे कुछ मुसलमान दोस्त अपनी हद तक उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानकारी कम होने की वजह से हम उन लोगों को पूरी तरह मुतमइन नहीं कर पाते। अगर आप इस मामले में हमारी रहनुमाई करें और इस मसले पर ऐसी जानकारी और दलीलें जुटा दें जिनसे कई शादियाँ करना (बहुविवाह) और ख़ास तौर पर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कई शादियों का सही होना वाज़ेह (स्पष्ट) हो जाए, तो हमारी बहस और विचारों के आदान-प्रदान में आसानी पैदा हो जाएगी और हम इंशाअल्लाह हर विषय में बराबर की सतह पर अपने विचार रख सकेंगे।
जवाब
यह एक अजीबोग़रीब बात है कि आज की पश्चिमी क़ौमें कई शादियाँ करने (बहुविवाह) को मज़हबी और सामाजिक बुराई समझती हैं और उनकी पैरवी में कुछ मॉडर्न ख़याल मुसलमान भी इसपर नाक-भौं चढ़ाते हैं जबकि आज की ईसाइयत से पहले बहुविवाह को इनसानी इतिहास में दीनी (धार्मिक) और अख़लाक़ी लिहाज़ से कभी बुरा या नापसन्दीदा या परहेज़गारी के ख़िलाफ़ नहीं समझा गया। आप उन एतिराज़ करनेवालों से पूछिए और ख़ुद भी बाइबल को पढ़कर देख लीजिए कि उसमें हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हज़रत इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) हज़रत याक़ूब (अलैहिस्सलाम) और दूसरे नबियों की एक से ज़्यादा बीवियों का ज़िक्र (वर्णन) मौजूद है या नहीं? जिन लोगों को हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नौ शादियों पर एतिराज़ है, ताज्जुब है कि उन्हें बाइबल की बयान की हुई इन रिवायतों पर कोई एतिराज़ नहीं है?
असल बात यह है कि आज की पश्चिमी क़ौमों पर एक तरफ़ सेक्स की तरफ़ झुकाव और लगाव है और दूसरी तरफ़ इस्लाम से नफ़रत व जिहालत पूरी तरह मुसल्लत है। इसलिए वे यह समझने पर मजबूर हैं कि बीवियों का मक़सद सिर्फ़ शहवानी जज़्बात (कामुक भावनाओं) की तस्कीन है, लेकिन जो शख़्स भी घरेलू ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ इस्लाम की तालीमात और हज़रत मुहम्मद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सीरत और जीवनी का खुले दिल से सूझ-बूझ के साथ मुताला करेगा, उसे यह बात आसानी से मालूम हो सकती है कि इस्लाम ने शादी का हुक्म देते हुए बहुत सारे अहम सामाजिक मक़सदों को अपने सामने रखा है और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कोई निकाह सिर्फ़ निकाह के लिए नहीं किया, बल्कि हर एक निकाह में कोई न कोई मस्लिहत और इस्लाम का इज्तिमाई फ़ायदा छिपा हुआ था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सबसे पहली शादी हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से की जो औलादवाली, विधवा और उम्र में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पन्द्रह साल बड़ी थीं। इस शादी के वक़्त नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उम्र 25 साल और हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की उम्र चालीस साल थी। उस नौजवानी में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सीरत इतनी पाक-साफ़ और बेदाग़ थी, जिसको इस्लाम के इनकारी भी मानते थे। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जब इस्लाम की दावत की शुरुआत की तो उससे रोकने के लिए मुशरिकों ने जो आपसी सुलह की पेशकश की थी उसमें यह बात भी शामिल थी कि आपकी शादी हिजाज़ (अरब का वह इलाक़ा जिसमें मक्का, मदीना और तायफ़ शामिल है) की सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत औरत से कर दी जाएगी, मगर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे बहुत ही हक़ीर (तुच्छ) समझते हुए ठुकरा दिया। हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अख़लाक़ और अमानतदारी से मुतास्सिर (प्रभावित) होकर नबी होने के एलान से पहले ही ख़ुद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से शादी की दरख़ास्त की थी। हालाँकि इस उम्र में दूसरी शादी करने की ज़रूरत और ख़ाहिश न रखती थीं। ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) एक दौलतमन्द औरत थीं और शादी के बहुत-से पैग़ामों को ठुकरा चुकी थीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी अगर चाहते तो किसी नौजवान कुँवारी लड़की से शादी कर सकते थे, मगर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की पाक-साफ़ सीरत की वजह से उनसे शादी की और जब तक हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) जीवित रहीं, पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दूसरी शादी नहीं की। इतिहास गवाह है कि यह शादी बहुत ही ख़ैर व बरकत का ज़रीआ बनी। हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नुबूवत मिलने के बाद सबसे पहले ईमान लाईं और अपनी जान-माल को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पाक ज़ात के लिए और सारी ज़िन्दगी के लिए वक़्फ़ कर दिया।
हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की वफ़ात (मृत्यु) के बाद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक दूसरी बूढ़ी विधवा औरत हज़रत सौदा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से शादी की, ताकि वे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कम उम्र बेटियों की तरबियत और निगरानी कर सकें और दूसरे घरेलू काम-काज की ज़िम्मेदारी भी निभाएँ। हज़रत सौदा (रज़ियल्लाहु अन्हा) निहायत पुख़्ता किरदार की मालकिन थीं। उन्होंने सिर्फ़ इस्लाम के लिए हब्शा को हिजरत की थी और बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेली थीं। चार साल तक अकेले वही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बीवी रहीं। इसके बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह ज़रूरी समझा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकाह में कोई ऐसी कम उम्र की औरत दाख़िल हो जिसने अपनी आँख इस्लामी माहौल ही में खोली हो और जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घराने में आकर परवान चढ़े ताकि उसकी तालीम व तरबियत हर लिहाज़ से मुकम्मल और मिसाली तरीक़े पर हो और वह मुसलमान औरतों और मर्दों में इस्लामी तालीमात के फैलाने का असरदार साधन बन सके। चुनाँचे इस मक़सद के लिए अल्लाह की मंशा ने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को चुना। उनके माँ-बाप का घर तो पहले ही से इस्लाम के नूर से रौशन था। फिर भी बचपन ही में उन्हें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घर पहुँचा दिया गया ताकि उनके कोरे काग़ज़ के समान दिल पर इस्लामी तालीम की गहरी और अमिट छाप लग जाए। चुनाँचे हम देखते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अपनी उसी नवउम्री में किताब व सुन्नत के ज्ञान में गहरी समझ हासिल की। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बेहतरीन किरदार, आमाल और फ़रमानों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने दिमाग़ में सुरक्षित रखा और तालीम व तरबियत और नक़ल व रिवायत के ज़रिये से उसे पूरी उम्मत के हवाले कर दिया। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के अपने कथनों और विचारों के अलावा उनसे दो हज़ार दो सौ दस (2210) सहीह मरफ़ूअ हदीसें रिवायत (बयान) की गईं हैं। अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) को छोड़कर सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और सहाबियात (रज़ियल्लाहु अन्हुन्न) में से किसी की रिवायत की हुई हदीसें इससे ज़्यादा नहीं हैं। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के कोई औलाद न थी। आप (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने बहुत-से बच्चों को अपनी तरबियत में लेकर उनको पाला-पोसा और उन्हें इल्म सिखाकर आलिम और आलिमा बना दिया।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दावत सिर्फ़ तबलीग़ और नसीहतों तक महदूद न थी, बल्कि यह एक सरफ़रोशाना (जान की बाज़ी लगा देने वाली) जिद्दोजुहद की बुनियाद थी जिसका मक़सद निज़ामे-ज़िन्दगी (जीवन-व्यवस्था) में अमलन इंक़िलाब बरपा करना था। ऐसे हालात में यह बात बहुत अहमियत रखती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बहुत क़रीबी और बहुत ही मुख़्लिस साथियों के साथ शादी-ब्याह के ताल्लुक़ात क़ायम करके उन्हें समाज में मुमताज़ (विशिष्ट) कर दें। चुनांचे एक तरफ़ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से अपनी प्यारी बेटियों की शादी कर दी और दूसरी तरफ़ हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की प्यारी बेटियों को अपने निकाह में लेकर चारों से अपने ताल्लुक़ को हमेशा के लिए क़ायम कर लिया। इसी तरह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने असर रखने वाले और नवमुस्लिम कुछ क़बीलों से भी रिश्तेदारी क़ायम करके उन्हें इस्लाम का हामी (समर्थक) बनाया और उनमें जो लोग मुख़ालिफ़ थे उनका विरोध ठण्डा कर दिया। हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) एक मोमिना, सादिक़ा और बहादुर औरत थीं, मगर बनू-मख़ज़ूम के उस ख़ानदान से थीं जिसका एक आदमी अबू-जहल था। हज़रत उम्मे-हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने इस्लाम की राह में जिस तरह अपनी जान जोखिम में डाली थी और जो जाँनिसारी और साबित-क़दमी दिखाई थी उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं, मगर उनका बाप अबू-सुफ़ियान मक्का फ़तह होने तक इस्लाम की मुख़ालिफ़त करने-वालों का सरदार था। इन दोनों ऊँचे मरतबेवाली औरतों को अपने निकाह में लेना उनके ज़ाती गुणों का एतिराफ़ भी था और इसका एक नतीजा यह भी निकला कि उन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी से भरी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गईं।
कुछ तलाक़ पाई हुई सहाबियात (रज़ियल्लाहु अन्हुन्न) को उनकी दिलजोई की ख़ातिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने निकाह में लिया। मुतबन्ना (मुँहबोला बेटा) को सगे बेटे जैसा बनाने की जाहिलाना रस्म को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह ने अपने मुँहबोले बेटे हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तलाक़ दी हुई बीवी हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) बिन्ते-जह्श से शादी करने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की फूफीज़ाद बहन थीं, अगर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते तो हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पहले ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) को अपने निकाह में ले लेते। मगर आपने ख़ानदान और ज़ात-पात की ऊँच-नीच को मिटाने के लिए उनका निकाह एक आज़ाद किए हुए ग़ुलाम से किया। फिर जब उस जोड़ में निबाह न हो सका और नौबत तलाक़ तक पहुँची तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत ज़ैनब को अपने निकाह में लेकर उनके दिली सुकून का सामान भी कर दिया और जाहिलियत के उस रिवाज की जड़ भी काट दी जिसकी वजह से मुतबन्ना (लैपालक) हक़ीक़ी औलाद की तरह समझा जाता था। उन्हीं की एक हमनाम हज़रत ज़ैनब बिन्ते-ख़ुज़ैमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) थीं जो हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-जहश के निकाह में थीं। ये हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) के तीसरे शौहर थे और उहुद की जंग में उन्होंने शहादत पाई थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनके ज़ख़्मी दिल पर मरहम रखते हुए उनको भी निकाह में ले लिया और इस सौभाग्य को पाने के बाद ये सिर्फ़ दो-तीन महीने ज़िन्दा रहकर जन्नत में जा बसीं। यहाँ यह बात भी ज़िक्र करने के लायक़ है कि हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के शौहर अबू-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने भी उहुद की जंग में ज़ख़्मी होकर शहादत पाई थी और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसके बाद हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से शादी करके उनके चार छोटे-छोटे बच्चों को अपनी हिफ़ाज़त और तरबियत में ले लिया था। इसी तरह हज़रत उम्मे-हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के शौहर ने अगरचे हबशा की तरफ़ उनके साथ हिजरत की थी, मगर वहाँ जाकर ईसाई हो गए और उम्मे-हबीबा अपनी छोटी बच्ची हबीबा के साथ बेघर और बेसहारा होकर रह गईं। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें हबशा ही में शादी का पैग़ाम भिजवाया। नज्जाशी ने ख़ुद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वकील के ज़रिये से निकाह का इन्तिज़ाम कराया और हज़रत उम्मे-हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास भिजवाया। हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) भी अपनी माँ के साथ आईं और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सौतेली बेटी बनकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सरपरस्ती में पली-बढ़ीं।
हज़रत जुवैरिया (रज़ियल्लाहु अन्हा) बनू-मुस्तलिक़ के सरदार हारिस-बिन-अबी-ज़िरार की बेटी थीं और मरीसीअ की जंग में क़ैद होकर आईं और एक सहाबी साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) बिन-क़ैस के हिस्से में आईं। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनकी ख़ानदानी शराफ़त का एहसास करके उनका फ़िदया ख़ुद दिया और उन्हें आज़ाद करके उनसे शादी कर ली। इसका असर यह हुआ कि तमाम सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने उनके क़बीले के सारे क़ैदियों को रिहा कर दिया जिनकी तादाद सौ से ज़्यादा थी।
इसी तरह का मामला हज़रत सफ़िया (रज़ियल्लाहु अन्हा) का भी है। वे भी जंगी क़ैदियों में से थीं और शुरू में हज़रत दिहिया कल्बी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हिस्से में आई थीं। मगर उनका बाप भी यहूदियों का सरदार था, इसलिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें भी आज़ाद करके ख़ुद उनसे शादी की ताकि उनका दिल टूटने न पाए और इस रिश्ते की वजह से यहूदियों की दुश्मनी भी कम हो जाए।
बहरहाल, जहाँ तक भी ग़ौर किया जाए, यह हक़ीक़त बिल्कुल स्पष्ट और साफ़ होकर सामने आती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जितनी भी शादियाँ की हैं, हर एक में कोई न कोई दीनी या मिल्ली मस्लिहत और हिकमत ही सामने थी। बल्कि हर एक में अनेकों मस्लिहतें पेशे-नज़र थीं। और यह बात भी ऐतिहासिक रूप से साबित है कि हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के अलावा तमाम की तमाम बीवियाँ (रज़ियल्लाहु अन्हुन्न) बेवा, तलाक़शुदा या शौहरदीदा थीं, लेकिन जिन लोगों के दिलो-दिमाग़ पर औरत का सिर्फ़ जिंसी पहलू सवार है और जिनकी नज़र पेट और जिंस के मसलों की हद से आगे नहीं हो सकती, वे अगर उन मस्लिहतों को न देख सकें जो प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शादियों में कारफ़रमा थीं तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये वे लोग हैं जिनके यहाँ शादी से पहले और शादी के बाद भी ग़ैर औरत-मर्दों से जिंसी ताल्लुक़ात रखना और बीवी की मौजूदगी में भी रखेलें रखना आम बात बन चुकी है, और ये इस्लाम के बहुविवाह-सिस्टम पर एतिराज़ करते हैं!!
(तर्जमानुल-क़ुरआन, मई 1968 ई.)
परदे पर एक औरत के सवाल और उनका जवाब
सवाल
मैं आपकी किताब 'रिसाला दीनियात' का अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ रही थी। पेज 182 तक मुझे आपकी तमाम बातों से इत्तिफ़ाक़ था। इस पेज पर पहुँचकर मैंने आपकी यह इबारत देखी “अगर औरतें ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें तो सादा कपड़े पहनकर और जिस्म को अच्छी तरह ढाँककर निकलें, चेहरा और हाथ खोलने की बहुत ज़रूरत न हो तो उनको भी छिपाएँ।" और इसके बाद दूसरे ही पेज पर यह इबारत मेरी नज़र से गुज़री "कोई औरत चेहरे और हाथ के सिवा अपने जिस्म का कोई हिस्सा (सिवाय शौहर के) किसी के सामने न खोले; चाहे वह उसका क़रीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो।" मुझे पहले तो आपकी इन दोनों इबारतों में तज़ाद (विरोधाभास) नज़र आता है। दूसरे आपका पहला बयान मेरे नज़दीक क़ुरआन मजीद की सूरा नूर, आयत 24 के ख़िलाफ़ है और उस हदीस से भी मुताबक़त (अनुकूलता) नहीं रखता जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत असमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया था कि लड़की जब बालिग़ हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा हाथ और चेहरे के सिवा नज़र न आना चाहिए।
किताब के आख़िर में आपने लिखा है कि "शरीअत के क़ानून किसी ख़ास क़ौम और ख़ास ज़माने के रस्म व रिवाज पर क़ायम नहीं हैं और न किसी ख़ास क़ौम और ख़ास ज़माने के लिए हैं।" मगर क़ुरआन के पढ़ने से यह साफ़ मालूम होता है कि परदा केवल एक रिवाजी चीज़ है और उसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आप यह मानेंगे कि आपने इस्लामी क़ानून का ग़लत मतलब बयान करके बहुत-से लोगों को इस्लाम से फिर जाने का सामान किया है? हम यह नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह पेश किया जाए जिससे इस ज़माने के नौजवान उसको क़बूल करने से भागें। इस्लाम की लागू की गई पाबन्दियों से बढ़कर अपनी तरफ़ से कुछ पाबन्दियाँ लगाने का किसी को क्या हक़ है?
(यह एक मुसलमान औरत के अंग्रेज़ी ख़त का तर्जमा है जो अमेरिका से आया था।)
जवाब
मैं आपकी साफ़गोई की क़द्र करता हूँ। लेकिन मेरा ख़याल है कि आपने पूरी तरह मेरी बात को नहीं समझा। पेज 182 और 183 पर जो कुछ मैंने कहा है उसमें आपस में कोई टकराव नहीं है। औरत के लिए शरीअत के हुक्म तीन हिस्सों में है।
• चेहरे और हाथ के अलावा बदन के दूसरे हिस्सों को शौहर के सिवा किसी के सामने औरत को न खोलना चाहिए, क्योंकि वे 'सतर' हैं और सतर (छिपाने के अंग) सिर्फ़ शौहर ही के सामने खोलना चाहिए।
• चेहरे और हाथ उन तमाम रिश्तेदारों के सामने खोले जा सकते हैं, और औरत अपनी ज़ीनत (श्रृंगार) के साथ उन तमाम रिश्तेदारों के सामने आ सकती है जिनका ज़िक्र क़ुरआन की सूरा नं. 24, आयत नं. 31 में किया गया है।
• उन रिश्तेदारों के सिवा आम अजनबी मर्दों के सामने औरत को अपनी ज़ीनत भी छिपानी चाहिए, जैसा कि ऊपर ज़िक्र की गई आयत में बयान किया गया है, और अपने चेहरे को भी छिपाना चाहिए जैसा कि क़ुरआन की सूरा 33 आयत नं. 53 से 55 और आयत 59 में बयान किया गया है।
अंग्रेज़ी में तर्जमा करनेवाले इन आयतों का तर्जमा करने में आमतौर पर घपला कर देते हैं, लेकिन अगर आप अरबी जानती हैं तो आपको ख़ुद ये आयतें अस्ल अरबी में देखनी चाहिएँ। उनको पढ़ने से साफ़ मालूम हो जाता है कि क़ुरआन मजीद शौहर, रिश्तेदारों और अजनबी मर्दों के बारे में औरतों के लिए अलग-अलग हदें मुक़र्रर करता है, और अजनबी मर्दों से उनको पूरा परदा करने का हुक्म देता है।
आपका यह ख़याल सही नहीं है कि परदा सिर्फ़ लोगों की 'रस्म' पर आधारित है। क़ुरआन के आने से पहले अरब वाले हिजाब (परदे) के तसव्वुर से बिल्कुल नावाक़िफ़ थे। यह क़ायदा सबसे पहले क़ुरआन मजीद ही ने उनके लिए मुक़र्रर किया। और बाद में सिर्फ़ मुसलमानों ही के अन्दर परदे का रिवाज रहा। दुनिया की कोई दूसरी क़ौम इसकी पाबन्द न थी और न है। आख़िर आपके नज़दीक वह किसकी 'रस्म' है जो परदे की सूरत में मुसलमानों के अन्दर चलन में आई?
आपका यह ख़याल सही है कि बेजा पाबन्दियाँ किसी को अपनी तरफ़ से बढ़ाने का हक़ नहीं है। मगर जो पाबन्दियाँ क़ुरआन और हदीस से साबित हैं, किसी मुसलमान को मॉडर्निज़्म में पड़ कर उन्हें तोड़ने की फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप उर्दू जानती हैं या नहीं। अगर उर्दू किताबें पढ़ सकती हों तो मेरी किताब परदा, सूरा नूर और सूरा अहज़ाब की तफ़सीर पढ़ें। उनसे आपको मालूम हो जाएगा कि परदे का हुक्म क़ुरआन की किन आयतों और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की किन हदीसों पर आधारित हैं। आप यह भी जान लेंगी कि ये पाबन्दियाँ बाद के लोगों ने बढ़ा दी हैं या अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही ने उनको लागू किया है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, अक्तूबर, 1966 ई.)
परदा और अपनी पसन्द की शादी
सवाल
इस्लामी परदे से जहाँ हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं वहाँ दो ऐसे नुक़सान हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि सब्र व शुक्र करके बैठ जाएँ।
पहला यह कि एक पढ़ा-लिखा शख़्स जिसकी एक ख़ास पसन्द है और जो अपने दोस्त चुनने में उनसे एक ख़ास अख़्लाक़ और पसन्द की उम्मीद रखता है, फ़ितरी तौर पर इसका ख़ाहिशमन्द होता है कि शादी के लिए जीवन-साथी भी अपनी मर्ज़ी से चुने। लेकिन इस्लामी परदे के होते हुए किसी नौजवान लड़के या लड़की के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं रहती कि वह अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन-साथी चुने बल्कि इसके लिए वे पूरे तौर पर दूसरों यानी माँ या ख़ाला (मौसी) वग़ैरह के भरोसे पर होते हैं। हमारी क़ौम की तालीमी हालत ऐसी है कि माँ-बाप आम तौर पर अनपढ़ और औलाद पढ़ी-लिखी होती है। इसलिए माँ-बाप से यह उम्मीद रखना कि सही मुनासिब रिश्ता ढूँढ लेंगे, बेकार की उम्मीद है। इस सूरते-हाल से एक ऐसा शख़्स जो अपने मसलों को ख़ुद हल करने और ख़ुद सोचने की ताक़त रखता हो सख़्त मुश्किल में पड़ जाता है।
दूसरी बात यह है कि एक लड़की जो घर से बाहर न निकलने की पाबन्द हो वह कैसे ऐसी सूझ-बूझ वाली अक़्लमन्द, और लोगों की परख रखने वाली हो सकती है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके और उनकी ज़ेहनी सलाहियतों को पूरी तरह से जगा दे। उसको तो दुनिया के मामलों का सही इल्म ही नहीं हो सकता, बल्कि सच्चाई यह है कि अगर वह उतनी ही तालीम भी हासिल कर ले जितनी एक बेपरदा लड़की ने हासिल की हुई है तो भी उसकी ज़ेहनी सतह कम होगी क्योंकि उसे अपने इल्म को अमली तौर पर परखने का कोई मौक़ा ही हासिल नहीं? उम्मीद है आप इस मसले पर रौशनी डालकर शुक्रिया का मौक़ा देंगे।
जवाब
आपने इस्लामी परदे की जिन ख़राबियों का ज़िक्र किया है, पहली बात तो वे ऐसी ख़राबियाँ नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पर आदमी ऐसी मुश्किलों में पड़ जाए जिनका कोई हल न हो और दूसरी बात यह कि दुनियावी ज़िंदगी में आख़िर कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई न कोई ख़ामी या कमी न पाई जाती हो। लेकिन किसी चीज़ के फ़ायदेमन्द या नुक़सानदेह होने का फ़ैसला उसके सिर्फ़ एक या दो पहलुओं को सामने रखकर नहीं किया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि कुल मिलाकर उसमें ज़्यादा ख़ूबियाँ हैं या ख़ामियाँ। यही उसूल परदे के बारे में अपनाया जाएगा। इस्लामी परदा आपकी राय में भी अनगिनत फ़ायदे अपने अन्दर रखता है, लेकिन सिर्फ़ यह मुश्किल कि उसकी पाबन्दी से आदमी को शादी के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ लड़की चुनने की आज़ादी नहीं मिल सकती। परदे के फ़ायदे को कम या उसकी पाबन्दी को छोड़ देने का जायज़ सबब नहीं बन सकता। बल्कि अगर हर लड़के को लड़की के चुनाव और हर लड़की को लड़के के चुनने की खुली छूट दे दी जाए तो इससे इतने भयानक नतीजे सामने आएँगे कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और फिर ख़ानदानी निज़ाम, जो कि समाज की मज़बूती और पाकीज़गी का ज़मानतदार होता है, बिखरकर रह जाएगा और एक ग़ैर हक़ीक़ी मुश्किल को दूर करते-करते बेशुमार हक़ीक़ी मुश्किलों के दरवाज़े खुल जाएँगे।
आपका यह ख़याल कि परदा करनेवाली लड़की सूझ-बूझ और अक़्ल से ख़ाली होती है; सही नहीं है, और अगर इसे सही मान भी लिया जाए तो इसमें परदे का कोई क़ुसूर नहीं है। एक लड़की परदे में रहकर भी इल्म व फ़न में कमाल हासिल कर सकती है और उसके मुक़ाबले में परदे से बाहर होकर भी एक लड़की इल्म, अक़्ल व सूझ-बूझ से कोरी रह सकती है। अलबत्ता बेपरदा लड़की को यह बड़ाई मिली हुई होगी कि वह मालूमात के लिहाज़ से चाहे ज़्यादा जानकारी न रखती हो लेकिन ताल्लुक़ात के लिहाज़ से उसकी नज़रें ज़रूर फैल जाएँगी। ऐसी हालत में अगर लायक़ और मुनासिब जीवन-साथी की तलाश में कामयाबी भी मिल जाए तब भी जो निगाहें फैलाव की आदी हो चुकी हों उन्हें समेटकर एक जगह महदूद (सीमित) रखना कोई आसान काम नहीं होगा।
क्या इस्लाम फ़ितरी दीन है?
सवाल
आपका जवाब मिला मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि आपने उसे बिल्कुल मामूली मसला ठहराया। कामयाब शादी की तमन्ना तो एक जाइज़ ख़ाहिश है और ऐसे हालात पैदा करना जिनकी वजह से एक आदमी के लिए अपनी पसन्द की लड़की चुनने का रास्ता बन्द हो जाए, मैं इनसानी ख़ुशियों और शख़्सियत की तरक़्क़ी के लिए नुक़सानदेह समझता हूँ और फ़ितरी दीन के ख़िलाफ़।
जहाँ तक मैं समझ सका हूँ हमारे यहाँ राइज तरीक़े के मुताबिक़ औरत ज़्यादा से ज़्यादा घर का इन्तिज़ाम करनेवाली और शौहर और ख़ुद अपने सेक्स की माँग को पूरा करने का ज़रीआ होती है। लेकिन दो लोगों के अपने आपको पूरी तरह एक-दूसरे के हवाले करने और ज़िन्दगी के फ़राइज़ (कर्तव्यों) को एक बार की बजाय ख़ुशी-ख़ुशी पूरा करने की जो सम्भावनाएँ अपनी पसन्द और ज़ौक़ की शादी करने में होती हैं वह इस सूरत में बिल्कुल मुमकिन नहीं कि अपनी पसन्द और समझ से काम लिए बग़ैर किसी दूसरे के कहने या पसन्द पर शादी कर ली जाए।
मेरा ख़याल है कि एक नौजवान सिर्फ़ सेक्स की माँग को पूरा करने का ख़ाहिशमन्द नहीं होता, वह यह भी चाहता है कि किसी के लिए कुछ त्याग करे, किसी से मुहब्बत करे, किसी की ख़ुशी का ख़याल रखे और कोई उसकी ख़ुशी पर ख़ुश हो। इस जज़्बे के फ़ितरी निकास का रास्ता तो यह है कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसे उसने तालीम, तौर-तरीक़ा, किरदार और दूसरी ख़ूबियों की बुनियाद पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हासिल किया है। (सच्ची मुहब्बत किसी की अन्दरूनी ख़ूबियों को देखने से ही पैदा होती है, न कि शक्ल-सूरत देख लेने से) और यह बात नामुमकिनों में से है कि पहले तो किसी की शादी करा दी जाए और फिर उससे मुतालबा किया जाए कि अब उसे ही चाहो और इस तरह चाहो जैसे तुमने उसको ख़ुद पसन्द किया है। इस फ़ितरी मुहब्बत का रास्ता बन्द कर लेने का नतीजा यह होता है कि यह जज़्बा (भाव) अपने लिए दूसरे रास्ते निकाल लेता है।
परदे की वजह से जो हालात पैदा हैं उनमें सही तौर पर किरदार देखकर वर तलाश करना मुमकिन नहीं। लड़के के बाप के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह लड़की का पता चला सके और लड़की की माँ के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह लड़के के बारे में ख़ुद कुछ अन्दाज़ा लगा सके; क्योंकि परदे की वजह से उन लोगों में भी ताल्लुक़ और आज़ाद होकर बात-चीत हो पाना नामुमकिन है। ख़ुद लड़के और लड़की का मिलना तो एक तरफ़ रहा, बड़ी-से-बड़ी आज़ादी जो इस्लाम ने दी है वह यह है कि लड़का लड़की की शक्ल देख ले। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसी की शक्ल कुछ सेकेण्ड देख लेने से क्या होता है।
इस मसले का एक और पहलू भी है। अब तो तमाम आलिमों ने यह मान लिया है कि मौजूदा तहज़ीब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इल्म का हासिल करना औरतों के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे एक ही काम कर सकती हैं। या तो इस्लामी हुक्मों की पाबन्दी करें या फिर इल्म हासिल करें। परदे की पाबन्द होते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि मेडिकल, आसारे क़दीमा (पुरातत्व), इंजीनियरिंग और तमाम ऐसे इल्म जिनमें सर्वे और दूरदराज़ सफ़र की ज़रूरत होती है, इन इल्मों के लिए औरतें किस तरह काम कर सकती हैं जबकि महरम (जिन मर्दों से परदा नहीं) के बग़ैर औरत का तीन दिन से ज़्यादा के सफ़र पर निकलना भी मना है, अब क्या हर जगह वह अपने साथ महरम को लिए-लिए फिरेगी?
ये तमाम इल्म तो एक तरफ़ रहे, मैं तो डॉक्टरी और परदे को भी एक-दूसरे की ज़िद (प्रतिकूल) समझता हूँ। एक तो डॉक्टरी की तालीम ही जो जिस्म की निगाहें फैला देनेवाली मालूमात से भरी होती है, शर्म व हया के उस एहसास को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है जिसकी पूर्वी औरतों से उम्मीद की जाती है, चाहे वह डॉक्टरी परदे ही में सीखी जाए और पढ़ानेवाली सारी औरतें ही क्यों न हों। दूसरे डॉक्टर बनने पर एक औरत को मरीज़ों के मिलने-जुलनेवालों से राबिता रखने की इस क़द्र ज़रूरत होती है कि उसके लिए ग़ैर मर्दों से बात-चीत पर रोक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके पेशे-नज़र अगर हम औरतों को डॉक्टरी पढ़ने या डॉक्टर बनने से रोकते हैं तो फिर हमें अपने घरों की मरीज़ औरतों के हर मर्ज़ के इलाज के लिए मर्द डॉक्टरों की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और इस वक़्त राइज हया-शर्म के मुताबिक़ यह तो इससे भी ज़्यादा बुरा समझा जाएगा।
जनाबे आली! आप मुझे यह बताएँ कि इन सामाजिक और तहज़ीबी उलझनों का इस्लामी हुक्मों की पाबन्दी करते हुए क्या हल है?
जवाब
आपका दूसरा ख़त मिला। शादी के मामले में आपने जो उलझन बयान की है वह अपनी जगह ठीक सही कि इसका हल कोर्टशिप के सिवा और क्या है? ज़ाहिर है कि जिस तफ़सील के साथ जीवन-साथी बनाने से पहले लड़की और लड़के को एक-दूसरे के औसाफ़ (गुणों) मिज़ाज, आदत, ख़सलत (स्वभाव) और पसन्द व ज़ेहन से वाक़िफ़ होने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, ऐसी तमाम बातों से वाक़िफ़ होना दो-चार मुलाक़ातों में और वह भी रिश्तेदारों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। इसके लिए महीनों एक-दूसरे के साथ मिलना, तनहाई में बात-चीत करना, घूमना-फिरना, सफ़र में एक-दूसरे के साथ रहना और बेतकल्लुफ़ दोस्ती की हद तक ताल्लुक़ पैदा होना ज़रूरी है। क्या वाक़ई आप यही चाहते हैं कि नौजवान लड़कों और लड़कियों के बीच इस मेल-मिलाप के मौक़े मिलने चाहिएँ? आपके ख़याल में उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के अन्दर उन मासूम फ़लसफ़ियों का फ़ीसदी (प्रतिशत) तनासुब (अनुपात) क्या होगा जो बड़ी संजीदगी के साथ सिर्फ़ अपने जीवन-साथी की तलाश में मुख़्लिस होकर अपना खोजी ताल्लुक़ क़ायम करेंगे और उस दौरान में शादी होने तक उस फ़ितरी खिंचाव और आकर्षण को क़ाबू में रखेंगे जो ख़ुसूसियत के साथ नौजवानी की हालत में औरत और मर्द एक-दूसरे के लिए अपने अन्दर रखते हैं? बहस बराए बहस अगर आप न करना चाहते हों तो आपको मानना पड़ेगा कि शायद दो-तीन प्रतिशत से ज़्यादा ऐसे लोगों का औसत हमारी आबादी में न निकलेगा। बाक़ी इस इम्तिहानी दौर ही में फ़ितरत के तक़ाज़े पूरे कर चुके होंगे और वे दो-तीन फ़ीसदी जो इससे बच निकलेंगे वे भी इस सन्देह से न बच सकेंगे कि शायद वे भी अपने फ़ितरी तक़ाज़े एक-दूसरे से पूरे कर चुके हों।
फिर क्या यह ज़रूरी है कि हर लड़का और लड़की जो इस तलाश व खोजबीन के लिए आपस में घुला-मिला करेंगे वे ज़रूर ही एक-दूसरे को अपना जीवन-साथी चुन ही लेंगे? हो सकता है बीस प्रतिशत दोस्तियों का नतीजा शादी की सूरत में बरामद हो।
अस्सी प्रतिशत या कम से कम पचास प्रतिशत को दूसरे या तीसरे तजरिबे की ज़रूरत पड़ेगी। इस सूरत में उन ‘ताल्लुक़ात' की क्या पोज़ीशन होगी जो तजरिबे के दौरान में आगे निकाह (शादी) की उम्मीद पर पैदा हो गए थे और उन सन्देहों के क्या असर होंगे जो 'ताल्लुक़ात' न होने के बावुजूद उनके बारे में समाज में पैदा हो जाएँगे।
फिर आप यह भी मानेंगे कि लड़कों और लड़कियों के लिए उन मौक़ों के दरवाज़े खोलने के बाद चुनाव या पसन्द का मैदान आख़िरकार बहुत फैल जाएगा। एक लड़के की नज़र में सिर्फ़ एक ही लड़की न होगी जिसपर वह अपनी चुनावी नज़र क़ायम करके खोजबीन और इम्तिहान के मरहले तय कर लेगा। और इसी तरह लड़कियों में से भी हर एक के लिए एक ही लड़का इमकानी शौहर की हैसियत से इम्तिहान के तहत न होगा। बल्कि शादी की मण्डी में हर तरफ़ एक से एक दिल लुभावन माल मौजूद होंगे जो इम्तिहानी मरहलों से गुज़रते हुए हर लड़के और हर लड़की के सामने बेहतर चुनाव के इमकान (सम्भावना) पैदा करते रहेंगे। इसी वजह से इस मामले के इमकानात दिन-ब-दिन कम होते जाएँगे कि शुरू में जो दो शख़्स एक-दूसरे से आज़माइशी मुलाक़ातें शुरू करें वे आख़िर वक़्त तक अपनी उस आज़माइश को निबाहें और आख़िरकार उनकी आज़माइश शादी पर ख़त्म हो।
इसके अलावा यह एक फ़ितरी बात है कि शादी से पहले लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरे के साथ रोमांटिक ढंग का कोर्टशिप करते हैं, उनमें दोनों एक-दूसरे को अपने जीवन के रौशन और अच्छे पहलू ही दिखाते हैं। महीनों की मुलाक़ातों और गहरी दोस्ती के बावजूद उनके कमज़ोर पहलू एक-दूसरे के सामने पूरी तरह नहीं आते। इस दौरान में शहवानी (वासनात्मक) खिंचाव इतना बढ़ चुका होता है कि वे जल्दी से शादी कर लेना चाहते हैं, और इस ग़रज़ के लिए दोनों एक-दूसरे से ऐसे-ऐसे वफ़ादारी के वादे करते हैं, इतनी मुहब्बत और दीवानगी का इज़हार करते हैं कि शादी के बाद अमली ज़िन्दगी में वे आशिक़-माशूक़ के किरदार को ज़्यादा देर तक किसी तरह नहीं निबाह सकते, यहाँ तक कि जल्द ही एक-दूसरे से मायूस होकर तलाक़ की नौबत आ जाती है, क्योंकि दोनों उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते जो इश्क़ व मुहब्बत के दौर में उन्होंने एक-दूसरे से बाँध ली थीं और दोनों के सामने एक-दूसरे के वे कमज़ोर पहलू आ जाते हैं जो अमली ज़िन्दगी ही में ज़ाहिर हुआ करते हैं, इश्क़-मुहब्बत के दौर में कभी नहीं खुलते।
अब आप उन पहलुओं पर भी ग़ौर करके देख लें, फिर आप मुसलमानों के मौजूदा तरीक़े की सोची हुई ख़राबियों और उस कोर्टशिप के तरीक़े की ख़राबियों के बीच मुक़ाबला करके ख़ुद फ़ैसला करें कि आपको इन दोनों में से कौन-सी ख़राबी ज़्यादा क़ाबिले क़बूल नज़र आती है। अगर इसके बाद भी आप कोर्टशिप ही को ज़्यादा क़ाबिले क़बूल समझते हैं तो मुझसे बहस की ज़रूरत नहीं है। आपको ख़ुद यह फ़ैसला करना चाहिए कि इस इस्लाम के साथ आप अपना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या नहीं, जो इस रास्ते पर जाने की इजाज़त देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह काम आपको करना हो तो कोई दूसरा समाज तलाश करें। इस्लाम से सरसरी जानकारी भी आपको यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस मज़हब की हद में “कामयाब शादी” का वह नुस्ख़ा इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिसे आप जाइज़ करना चाहते हैं।
औरतों की तालीम के मुताल्लिक़ आपने जिन कठिनाइयों को बयान किया है उनके बारे में भी कोई राय क़ायम करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि फ़ितरत ने औरत और मर्द के काम करने या ज़िम्मेदारी निभाने का दायरा अलग-अलग रखा है। अपने दायरे की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए औरत को जिस अच्छी-से-अच्छी तालीम की ज़रूरत है वह उसे ज़रूर मिलनी चाहिए और इस्लामी हदों में रहकर वह पूरी तरह दी जा सकती है। इसी तरह औरत के लिए ऐसी इल्मी व ज़ेहनी तरक़्क़ी भी उन हदों के अन्दर रहते हुए मुमकिन है जो औरत को अपने दायरे की ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाते हुए हासिल हो सकती है। इस मामले में कोई इन्तिज़ाम न करना मुसलमानों की अपनी कोताही है न कि इस्लाम की। लेकिन वह तालीम जो मर्द के दायरे का काम करने के लिए औरत को तैयार करे, औरत ही के लिए नहीं बल्कि पूरी इनसानियत को तबाह करनेवाली है और इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। इस मसले पर तफ़सील से जानने के लिए मेरी किताब 'परदा' का गहराई से अध्ययन करें।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जनवरी 1961 ई.)
जंग के मैदान में क़हबागिरी (वेश्यावृत्ति) का प्रबन्ध और इस्लाम
सवाल
आजकल जंग में सिपाहियों को वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और उनकी वापसी कम से कम दो साल से पहले नामुमकिन हो जाती है। सामाजिक बुराइयों, मिसाल के तौर पर ज़िना (व्यभिचार) वैग़रह का फैल जाना लाज़िम है क्योंकि जंग की भावना की बेदारी के साथ तमाम सेक्स की भावनाएँ भी भड़क उठती हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए या क़ाबू में लाने के लिए फ़ौजों के लिए रजिस्टर्ड वेश्याएँ (तवायफ़ Sexworkers) साथ रखने की स्कीम पर अमल हो रहा है और उनके दिलों को ख़ुश रखने के लिए W.A.C.I. दफ़तरों में मुलाज़िम रखी जा रही हैं। ये दोनों सूरतें लानत के क़ाबिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनको रद्द करने के बाद इस्लाम इस मसले के हल का क्या तरीक़ा बताता है। कनीज़ों (दासियों) का सिस्टम किस हद तक इस बुराई से छुटकारा दिला सकता है और क्या वह भी एक तरह की जाइज़ की हुई वेश्यावृत्ति (Prostitution) नहीं है?
जवाब
आपके सवाल में एक पेचीदगी है जिस को शायद आपने अपना सवाल लिखते वक़्त महसूस नहीं किया। आप जिस मसले का हल जानना चाहते हैं उसमें आपके पेशे-नज़र तो हैं मौजूदा ज़माने की फ़ौजें और उनकी ज़रूरतें, लेकिन इसका हल चाहते हैं आप इस्लाम से। हालाँकि इस्लाम जिन फ़ौजों की ज़रूरतों का ज़िम्मा लेता है वे उसकी अपनी फ़ौजें हैं, न कि हरामकारों, बदकिरदारों और ज़ालिमों की फ़ौजें।
मौजूदा ज़माने की फ़ौजों का हाल यह है कि उन्हें सिर्फ़ लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। जो हुकूमतें उनको तैयार करती हैं उनकी नज़र के सामने कोई पाकीज़ा अख़लाक़ी मक़सद नहीं होता। अगर वे अपनी क़ौमी फ़ौज तैयार करती हैं तो उनके अन्दर सिर्फ़ ऐसे अख़्लाक़ और किरदार पैदा करने की कोशिश करती हैं जो देश का झण्डा ऊँचा करने और ऊँचा रखने के लिए दरकार हैं, और ज़ाहिर है कि उन किरदारों में पाकीज़ा किरदार के तत्त्व की कोई जगह नहीं है, और अगर वे अपनी महकूम (पराजित) क़ौमों में से अपने फ़ायदे के लिए फ़ौजें तैयार करती हैं तो उन्हें सिर्फ़ उन अख़लाक़ की तरबियत देती हैं जो पालतू शिकारी कुत्तों में पैदा किए जाते हैं। यानी यह कि रोटी देनेवाले के वफ़ादार रहें और शिकार उसके लिए मारें, न कि अपने लिए। इसके सिवा किसी दूसरे अख़लाक़ की अहमियत सिरे से उन ‘मुहज्ज़ब' क़ौमों में है ही नहीं। रहीं ज़िना, शराब, जुआ और दूसरी क़िस्म की बदअख़्लाक़ियाँ तो नीचे से लेकर ऊँचे तबक़ों तक वे उनके यहाँ पूरी क़ौम के अन्दर फैली हुई हैं। अब जबकि उनका अख़्लाक़ी नुक़्त-ए-नज़र ही यह है कि “खाओ, पियो और मौज करो, दुनिया दोबारा मिलनेवाली नहीं" तो कोई वजह नहीं कि उनकी फ़ौजों में किसी प्रकार का अख़लाक़ी लगाव और जमाव पाया जाए।
यही वजह है कि उनकी फ़ौजें मार-धाड़ के फ़न में इन्तिहाई कमाल दर्जे तक पहुँच जाती हैं। लेकिन पाकीज़ा अख़लाक़ के नुक़्त-ए-नज़र से पस्ती की उस हद तक गिरी हुई होती हैं जिसका मुश्किल ही से कोई इनसान तसव्वुर कर सकता है। उन्हें खाने के लिए दिल खोलकर राशन दिया जाता है, पीने के लिए शराब के मटकों का मुँह हर वक़्त खुला रखा जाता है। ख़र्च करने के लिए पैसे भी काफ़ी दिए जाते हैं। फिर साँडों की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है कि अपने सेक्स की माँग जहाँ और जिस तरह चाहें पूरी करते फिरें। हुकूमतें ख़ुद भी उनके लिए वेश्यालय (चकले) तैयार रखती हैं। क़ौम की लड़कियों में भी यह जज़्बा पैदा किया जाता है कि वे देश व क़ौम के लिए लड़नेवाले सिपाहियों की ख़ातिर अपने जिस्म को ख़ुशी-ख़ुशी पेश करने को देश के लिए त्याग और फ़ख़्र की चीज़ समझें और इस पर भी जब उन इनसानी नरों की भड़की हुई कामवासनाएँ शान्त न हो सकें तो उनको पूरी आज़ादी हासिल होती है कि इनसानी गल्ले (भीड़) में जहाँ भी मादाएँ उनको नज़र आ जाएँ उनसे बलपूर्वक या माल देकर उनके जिस्म ख़रीद लें या छीन लें। इस तरह जिन फ़ौजों को पाला गया हो, ख़ुदा ही बेहतर जानता है कि जब वे अपने दुश्मनों के मुल्कों में फ़तह पाकर दाख़िल होती होंगी तो वहाँ उनकी सेक्स की माँगे कितनी बढ़ जाती होंगी और किस क़ियामत-खेज़ अंदाज़ में पूरी की जाती होंगी। [बोस्निया की जंग में इसकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। (संकलनकर्ता)]
अब आप ख़ुद ही सोच लें कि ऐसी फ़ौजों के मसलों और उनकी ज़रूरतों का हल इस्लाम कैसे बता सकता है। उन्हें पश्चिम ही के दुनियापरस्ताना अख़्लाक़ ने पैदा किया है और उनके शर्मनाक मसलों का हल भी वही पेश कर सकता है। इस्लाम जिन फ़ौजों को तैयार करता है वे सियासी, व मआशी (आर्थिक) भूगोल के पन्ने फाड़ने और जोड़ने के लिए नहीं तैयार की जातीं, बल्कि सिर्फ़ इसलिए तैयार की जाती हैं कि दुनिया अगर ख़ुदा की पैरवी से फिरी हुई हो और दावत व तबलीग़ और समझाने-बुझाने से सही राह पर न आए तो उसे तलवार की ताक़त से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वह कम-से-कम फ़ितना-फ़साद से तो बाज़ आ जाए। इस मुक़र्रर मक़सद के लिए जो फ़ौजें जिहाद करती हैं, उनका जिहाद ख़ाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि ख़ुदा की राह में होता है। वे जंग के मैदान में भी उसी इबादत की भावना से जाती हैं जिस भावना के साथ वे मस्जिद के अन्दर क़दम रखती हैं। फिर इस मैदान में उनको उतारने से पहले मन को शुद्ध करने और अख़्लाक़ को पाक-साफ़ रखने के एक पूरे कोर्स से उन्हें गुज़ारा जाता है। उन्हें ख़ुदा से फिरे हुए लोगों के सिर को कुचलने का काम सिखाने के साथ यह भी सिखाया जाता है कि वे अपने नफ़्स (मन) को, अगर वह ख़ुदा से फिरा हुआ हो, किस तरह क़ाबू में करें। दूसरों को ख़ुदा के हुक्मों का पाबन्द बनाने से पहले ख़ुद अपने आपको किस तरह ख़ुदा का हुक्म माननेवाला बनाएँ। उन्हें यह सिखाया जाता है कि जंग के मैदान में क़दम-क़दम पर ख़ुदा को याद करते हुए बढ़ें। लड़ाई की हालत तक में नमाज़ अपने वक़्त पर अदा करें और दिन उनके घोड़े या टैंक की पीठ पर गुज़रें तो रातें मुसल्ले पर। ज़ाहिर है कि इस तरह की तरबियत पाई हुई फ़ौज जो एक पाकीज़ा अख़लाक़ी मक़सद के लिए लड़े और अपने अक़ीदे के मुताबिक़ जंग के ज़माने को इबादत का ज़माना समझती हुई जंग के मैदान में रहे। उसकी शहवानी (वासनात्मक) माँगें मौजूदा फ़ौजों की माँगों की तरह नहीं हो सकतीं और न वे अपनी इन माँगों को पूरा करने में उन फ़ौजों की तरह आज़ादी की ख़ाहिशमन्द हो सकती हैं।
हालाँकि कुछ रिवायतों के मुताबिक़ जंग के ज़माने में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ‘मुतआ' [कुछ मुद्दत के लिए किसी औरत से निकाह कर लेना।] जायज़ (वैध) रखा था (जिसे अरब में पहले जायज़ समझा जाता था) लेकिन यह बात साबित है कि जल्द ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इससे रोक दिया।
इसमें शक नहीं कि जो औरतें जंग में गिरफ़्तार हुई हों उनसे सेक्स करने की इजाज़त इस्लाम में दी गई है। मगर बड़ा जाहिल है वह आदमी जिसने इसका मतलब यह समझा कि जिस तरह आज की नास्तिक फ़ौजें महकूम (परास्त) के मुल्क में घुसने के बाद औरतों को आज़ादाना पकड़ती फिरती हैं और जहाँ जिस सिपाही को जो औरत मिल जाती है वह उससे ज़िना (सेक्स) कर डालता है, ऐसी ही इजाज़त इस्लाम ने भी अपनी फ़ौजों को दे दी है। अस्ल में यह इजाज़त कुछ शर्तों के साथ है।
पहली बात तो यह है कि औरतों को पकड़ना अपने आप में अस्ल मक़सद की हैसियत नहीं रखता कि ख़ाहमख़ाह फ़ौज की शहवानी ज़रूरतें पूरी करने की ख़ातिर दुश्मन क़ौम की औरतों को भेड़-बकरियों की तरह पकड़ लाया जाए, बल्कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और 'ख़िलाफ़ते-राशिदा' के ज़माने की मिसालों से साफ़ मालूम होता है कि औरतें जब कभी गिरफ़्तार होंगी तो दो ही सूरतों में होंगी—एक इस सूरत में जबकि वे दुश्मन के लश्कर में हों। इस सूरत में जिस तरह लश्कर के मर्द गिरफ़्तार होंगे उसी तरह औरतें भी गिरफ़्तार कर ली जाएँगी। दूसरे उस सूरत में जब कि कोई शहरी आबादी इस्लामी फ़ौज का मुक़ाबला करे और हमले में (By Storm) पराजित हो। इस सूरत में इस्लामी फ़ौज के कमांडर को अधिकार है कि ज़रूरत समझे तो पूरी आबादी को क़ैद कर ले। और इस सूरत में जो औरतें और बच्चे ऐसे रह जाएँ जिनके सरपरस्त मर्द मारे जा चुके हैं उनको भी इस्लामी फ़ौज अपने चार्ज में ले लेगी।
फिर जो औरतें इन सूरतों में से किसी सूरत में फ़ौज के क़ब्ज़े में आ जाएँ उन्हें कोई सिपाही उस वक़्त तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि इस्लामी हुकूमत इस बात का फ़ैसला न कर ले कि उन्हें लौंडियाँ बना लेना है, और जब तक कि उनको फ़ौज में बाक़ायदा तक़सीम (बाँट) न कर दिया जाए। और यह फ़ैसला सिर्फ़ उसी सूरत में किया जाएगा जबकि दुशमन से नक़द मुआवज़े पर, या जंगी क़ैदियों के तबादले पर कोई मामला तय न हुआ हो।
इस तरह जो औरत हुकूमत की तरफ़ से किसी मर्द की मिलकियत में बाक़ायदा दे दी गई हो तो सिर्फ़ वही एक मर्द उसका उपभोग (तसर्रुफ़) कर सकेगा। और उसके लिए भी क़ानून यह है कि गर्भ की परख की ख़ातिर वह उस वक़्त तक सब्र करे जब तक उस औरत को एक बार हैज़ (मासिक धर्म) न आ जाए। यह इस गरज़ के लिए है ताकि इस बात का पूरा यक़ीन हो जाए कि वह गर्भवती नहीं है। अगर वह गर्भवती हो तो फिर बच्चा पैदा होने तक उसको सब्र करना चाहिए। इस बीच में वह उससे सम्भोग (Sex) करने का हक़ नहीं रखता।
फिर जो औरत इस तरीक़े से किसी शख़्स के सुपुर्द की गई हो वह अगर उससे हमबिस्तरी करे तो जो औलाद उसके गर्भ से पैदा होगी वह उस शख़्स की जाइज़ औलाद क़रार पाएगी और उसकी वारिस होगी और इसके साथ ही उस औरत के माँ बन जाने के बाद फिर वह शख़्स उस औरत को बेचने का हक़दार न रहेगा और उसके मरने के बाद औरत ख़ुद-ब-ख़ुद आज़ाद हो जाएगी।
यह है जंग में पकड़ी हुई औरतों के बारे में इस्लाम का अस्ल क़ानून। इसके बाद कौन कह सकता है कि इस्लाम जंग की हालत में अपनी फ़ौजों को शहवानी (कामुक) ज़रूरतें पूरी करने के लिए अख़्लाक़ी बंदिशों में किसी क़िस्म की ढील देता है। इसके ख़िलाफ़ इस्लाम तो उनपर यह पाबन्दी लगाता है कि जाइज़ ताल्लुक़ बनाने के मौक़े मिलने तक हर हाल में अपनी कामवासना पर क़ाबू रखते हुए सब्र से काम लें, चाहे ऐसा मौक़ा मिलने में कितनी ही मुद्दत लग जाए।
दूसरी तरफ़ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के बयानों और उनकी ज़िंदगी के वाक़िआत और हदीसों का मुताला (अध्ययन) करने से मालूम होता है कि इनसानी कमज़ोरियों का लिहाज़ करते हुए यह देखना भी इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से है कि उसके सिपाही ज़्यादा मुद्दत तक अपनी औरतों से अलग रहकर और उनकी औरतें ज़्यादा देर तक अपने मर्दों से जुदा रह कर कहीं अख़्लाक़ी बुराइयों में न पड़ जाएँ। यही ग़रज़ थी जिसकी ख़ातिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया—
"मुजाहिदों की बीवियाँ पीछे रहनेवाले मर्दों के लिए वैसी ही हराम की गई हैं जैसी ख़ुद उनकी माएँ उनपर हराम हैं।"
और यह भी फ़रमाया—
“पीछे रह जानेवाले मर्दों में से जो शख़्स किसी मुजाहिद के बाल-बच्चों का सरपस्त बना हो और फिर वह उनके मामले में उसके साथ किसी क़िस्म की ख़ियानत करे वह क़ियामत के रोज़ खड़ा किया जाएगा और उस मुजाहिद को हक़ दिया जाएगा कि उस आदमी के अमल में से जो कुछ चाहे ले ले। फिर तुम्हारा क्या ख़याल है कि वह उसके पास कुछ छोड़ देगा?"
और यही वजह थी कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मदीना के दो ख़ूबसूरत नौजवानों को सिर्फ़ इसलिए शहर से निकालकर दूसरी जगह भेज दिया था कि आपने औरतों की ज़बान से उनके हुस्न की तारीफ़ सुन ली थी और आपको अन्देशा हो गया था कि कहीं यह चीज़ उन औरतों के हक़ में फ़ितना न बन जाए; जिनके शौहर जिहाद में गए हुए हैं। यही वजह थी कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एलान कर दिया था कि जो आदमी अपनी शेरो-शायरी में किसी औरत से इश्क़ का इज़हार करेगा उसको कोड़े मारे जाएँगे, और यही वजह थी कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जब एक बार एक मुजाहिद की बीवी को अपने शौहर की जुदाई में प्यार भरे गीत गाते हुए सुना तो आकर जो पहला हुक्म आपने जारी किया वह यह था कि आइंदा से सिपाहियों को इतनी लम्बी मुद्दत तक उनकी बीवियों से जुदा न रखा जाए, जिससे उनके किसी बदअख़लाक़ी में पड़ जाने का अंदेशा हो। दूसरे शब्दों में फ़ौज में रुख़सत (Furlough) का तरीक़ा इस्लामी हुकूमत में जारी ही इस ग़रज़ के लिए किया गया था कि हुकूमत अपने सिपाहियों और उनकी औरतों के अख़लाक़ की हिफ़ाज़त करना चाहती थी।
रहा आपका यह सवाल कि लौंडियों के इस्तेमाल की इजाज़त एक तरह की क्या जाइज़ की हुई वेश्वावृत्ति न थी? तो इसका जवाब यह है कि या तो आप वेश्यावृत्ति के मानी नहीं जानते या लौंडियों से सम्भोग करने का इस्लामी क़ानून आपको मालूम नहीं है। वेश्यावृत्ति उसे कहते हैं कि एक मर्द किसी औरत से उसका जिस्म किराए पर कुछ वक़्त के लिए माँग ले और आजकल मुहज़्ज़ब (सभ्य) सोसाइटी में एक नई क़िस्म की वेश्यावृत्ति पैदा हो गई है जिसे “शौक़िया वेश्यावृत्ति” (Amateurish Prostitution) कहते हैं, जिसमें यही वक़्ती ताल्लुक़ तैयशुदा किराए के बदले में नहीं बल्कि उपहारों, और तोहफ़ों के बदले में क़ायम होता है और सोसाइटी में औरत की इज़्ज़त-आबरू पहले की तरह बरक़रार मानी जाती है। रहा कनीज़ों (लौंडियों) से हमबिस्तरी (Sex) करने का इस्लामी क़ानून तो वह मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, दोनों का मुक़ाबला करके आप ख़ुद देख लें।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, मार्च-जून-1945 ई.)
इस्लाम में ग़ुलामी को बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया?
सवाल
ग़ुलामी (दासता) से मुताल्लिक़ इस्लाम में ज़ाब्ते और क़ानून ऐसे बनाए गए हैं जिनसे अन्देशा होता है कि ग़ुलामी को हमेशा बाक़ी रखना मक़सूद है। मगर दूसरी तरफ़ ऐसे आदेश भी मौजूद हैं जिनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा गया था, बल्कि ग़ुलामों की रिहाई और आज़ादी ही महबूब और मनपसन्द थी। सवाल यह है कि जब ग़ुलामी नापसन्दीदा और आज़ादी पसन्दीदा थी तो इस तरीक़े को बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया?
जवाब
ग़ुलामी को बिल्कुल ख़त्म न कर देने की वजह यह है कि इस्लाम ने उसे सिर्फ़ एक जंगी-ज़रूरत की हैसियत से बाक़ी रखा है, और यह ज़रूरत हर ऐसे मौक़े पर पेश आ सकती है जबकि किसी दुश्मन से जंगी क़ैदियों के आपसी तबादले या नक़द मुआवज़े (फ़िदिए) पर हमारा समझौता न हो सके और हमारी हुकूमत जंगी क़ैदियों को बिना फ़िदिया और बिना बदला लिए छोड़ देना मुल्की मस्लिहतों और हिकमतों के ख़िलाफ़ समझे। एक दो घटनाओं को छोड़कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में अठारहवीं सदी ईसवी के अन्त तक जंगी क़ैदियों के आपसी तबादले का तरीक़ा राइज न था। न इस बात का कोई इमकान था कि मुसलमान हुकूमतें दुश्मन के जंगी क़ैदियों को छोड़कर अपने जंगी क़ैदियों को भी छुड़ा सकतीं। और अब अगर दुनिया में जंगी क़ैदियों के आपसी तबादले का तरीक़ा राइज हुआ है तो वह किसी धार्मिक आदेश की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक मस्लिहत की बुनियाद पर है, जिसे कोई क़ौम जब चाहे नज़रअन्दाज़ कर सकती है। आज यह नामुमकिन नहीं है कि हमारा किसी ऐसे हठधर्म दुश्मन से साबक़ा पेश आ जाए जो जंगी क़ैदियों के आपसी तबादले की तजवीज़ (प्रस्ताव) को ठुकरा दे और हमारे जंगी क़ैदियों को किसी शर्त पर भी छोड़ने के लिए राज़ी न हो। अब आप ख़ुद सोचें कि अगर इस्लाम हमें हर हालत में जंगी क़ैदियों की रिहाई का पाबन्द कर देता तो क्या यह हुक्म हमारे लिए मुसीबत की वजह न बन जाता? क्या कोई क़ौम भी हमेशा-हमेशा के लिए इस नुक़सान का बोझ उठा सकती है कि हर लड़ाई में उसके आदमी दुश्मन के पास क़ैद होते रहें और वह दुश्मन के आदमियों को छोड़ती चली जाए? और क्या कोई दुश्मन भी ऐसा बेवक़ूफ़ हो सकता है कि वह हमसे कभी जंगी क़ैदियों के आपसी तबादले का समझौता करने पर तैयार हो जबकि उसे यह पूरा यक़ीन हो कि हम हर हालत में अपने धार्मिक हुक्मों की वजह से उसके आदमियों को छोड़ने पर मजबूर हैं?
इस सिलसिले में एक सवाल पर और भी ग़ौर कर लीजिए। किसी व्यक्ति को उम्र भर जेल में रखना या उससे जबरी मेहनत (Forced Labour) लेना और उसे मौजूदा दौर के इनसानी बाड़ों (Concentration Camps) में रखना आख़िर किस दलील की बुनियाद पर ग़ुलामी से बेहतर समझा जा सकता है? ग़ुलामी में तो इसके मुक़ाबले में ज़्यादा आज़ादी हासिल रहती है। आदमी को शादी-ब्याह का मौक़ा भी मिल जाता है। एक आदमी को सीधे तौर पर एक आदमी से वास्ता पड़ता है जिसमें ज़्यादा इनसानी सुलूक का इमकान है और एक ग़ुलाम अपने आक़ा को ख़ुश करके या उसे फ़िदिया (मुआवज़ा) देकर आज़ादी भी हासिल कर सकता है। पहले ज़रा उस सुलूक का मुताला कर लीजिए जो रूस और जर्मनी में दुश्मन के जंगी क़ैदियों ही के साथ नहीं ख़ुद अपने मुल्क के सियासी 'मुजरिमों' के साथ भी किया गया है और किया जा रहा है। फिर फ़ैसला कीजिए कि अगर कभी किसी ऐसे दुश्मन से हमें साबक़ा पेश आ जाए और वह हमारे जंगी क़ैदियों के साथ यह सुलूक करने लगे तो क्या उसके जवाब में हम को भी यही जानवरों जैसा सुलूक करना चाहिए? या इससे बेहतर और ज़्यादा इनसानियत पर आधारित सुलूक वह है जो इस्लाम ने हमको ग़ुलामों के साथ करने की इजाज़त और हिदायत दी है?
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जून-जुलाई 1952 ई.)
इस्लामी हुकूमत में ज़िम्मी (ग़ैर-मुस्लिम) प्रजा
सवाल
मैं हिन्दू महासभा का वर्कर (कार्यकता) हूँ। पिछले साल..... प्रान्त की हिन्दू महासभा का प्रोपेगंडा (Propaganda) सेक्रेट्री चुना गया था। मैं हाल ही में आपके नाम से वाक़िफ़ हुआ हूँ। आपकी कुछ किताबें ‘मुसलमान और मौजूदा सियासी कश-मकश' (हिस्सा, 1 और 3), 'इस्लाम का नज़रिय-ए-सियासी', 'इस्लामी हुकूमत किस तरह क़ायम होती है', 'सलामती का रास्ता' [ये तमाम किताबें 'मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स' नई दिल्ली-25 से भी प्रकाशित हुई हैं।] वग़ैरह पढ़ी हैं। जिनके पढ़ने के बाद इस्लाम के बारे में मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया है और मैं निजी तौर पर यह ख़याल करता हूँ कि अगर यह चीज़ कुछ समय पहले हो गई होती तो हिन्दू-मुस्लिम मसला इतना ज़्यादा पेचीदा न होता। जिस इस्लामी हुकूमत की आप दावत दे रहे हैं उसमें ज़िन्दगी बसर करना फ़ख़्र (गर्व) की बात हो सकती है। मगर कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। ख़तो-किताबत (पत्र व्यवहार) के अलावा अगर ज़रूरत होगी तो मैं ख़ुद आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँगा।
सबसे पहली बात जो जानना चाहता हूँ वह यह है कि हिन्दुओं को इस्लामी हुकूमत के अन्दर किस दर्जे में रखा जाएगा? क्या उनको अहले-किताब के हक़ दिए जाएँगे या ज़िम्मी के? अहले-किताब और ज़िम्मी लोगों के हक़ों की तफ़सील इन किताबों में भी नहीं मिलती। मुझे जहाँ तक सिन्ध पर अरबी हमले के इतिहास का इल्म है मुहम्मद-बिन-क़ासिम और उसके जानशीनों ने सिन्ध के हिन्दुओं को अहले-किताब के अधिकार दिए थे। उम्मीद है कि आप इस मामले में तफ़सील के साथ अपने विचार पेश करेंगे।
आप यह भी बताइए कि अहले-किताब और ज़िम्मी के अधिकारों में क्या फ़र्क़ है। क्या वे देश की हुकूमत के इन्तिज़ाम में बराबर के भागीदार हो सकते हैं? क्या पुलिस, फ़ौज और क़ानून लागू करनेवाले गिरोह में हिन्दुओं का हिस्सा होगा? अगर नहीं तो क्या हिन्दुओं के अकसरियतवाले सूबों (राज्यों) में आप मुसलमानों के लिए वही हैसियत तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे जो कि आप इस्लामी हुकूमत में हिन्दुओं को देंगे?
दूसरी बात समझने की यह है कि क़ुरआन मजीद के फ़ौजदारी और दीवानी क़ानून क्या मुसलमानों की तरह हिन्दुओं पर भी लागू होंगे? क्या हिन्दुओं का क़ौमी क़ानून (Personal Law) हिन्दुओं पर लागू होगा या नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है कि हिन्दू अपने विरासती क़ानून, मुश्तरका फेमिली सिस्टम् (संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था) और दत्तक बनाने के (मनुस्मृति पर आधारित) नियमों के मुताबिक़ ज़िन्दगी बिता सकेंगे या नहीं? वाज़ेह रहे कि ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं कि हक़ीक़त का इल्म हो सके।
जवाब
मैं आपके उन ख़यालों की दिल से क़द्र करता हूँ जो आपने अपने ख़त में ज़ाहिर किए हैं। यह सच है कि हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम मसले को पेचीदा और नाक़ाबिले-हल हद तक पेचीदा बना देने की ज़िम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने सच्चाई के उसूलों और हक़ की बुनियादों पर ज़िन्दगी के मसलों को हल करने के बजाय शख़्सी, ख़ानदानी, तबक़ाती, नस्ली और क़ौमी बुनियादों पर उन्हें देखने और हल करने की कोशिश की। इसका अंजाम वही कुछ होना चाहिए था जो आज हम देख रहे हैं और इसी बदक़िस्मती में हम और आप सब बराबर के शरीक हैं। कोई भी फ़ायदे में नहीं है।
आपने जो सवाल किए हैं उनके मुख़्तसर तौर पर नम्बरवार जवाब नीचे दिए जा रहे हैं—
(1) अगर ख़ुदा के हुक्म की बुनियाद पर हुकूमत क़ायम हो तो उसकी हैसियत यह न होगी कि एक क़ौम दूसरी क़ौम या क़ौमों पर हाकिम है, बल्कि उसकी हैसियत यह होगी कि मुल्क पर एक उसूल (सिद्धांत) की हुकूमत क़ायम है। ज़ाहिर बात है कि ऐसी हुकूमत को चलाने की ज़िम्मेदारी मुल्क के बाशिन्दों में से वही लोग उठा सकेंगे जो उस उसूल और सिद्धांत को मानते हों। दूसरे जो लोग उस उसूल को न मानते हों या कम से कम उसपर मुत्मइन न हों उनको उस हुकूमत में क़ुदरती तौर पर "अहले-ज़िम्मा" की हैसियत हासिल होगी। यानी जिनकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी वे लोग लेते हैं जो उस उसूली हुकूमत को चलानेवाले हैं।
(2) “अहले-किताब" और "आम अहले-ज़िम्मा" के बीच इसके सिवा कोई फ़र्क़ नहीं है कि अहले-किताब की औरतों से मुसलमान शादी कर सकते हैं और दूसरे ज़िम्मियों (ग़ैर-मुस्लिम) की औरतों से नहीं कर सकते। लेकिन अधिकारों में उनके बीच कोई फ़र्क़ नहीं है।
(3) ज़िम्मियों के अधिकारों के बारे में तफ़सील तो मैं इस ख़त में नहीं दे सकता, अलबत्ता उसूली तौर पर आपको बताए देता हूँ कि ज़िम्मी दो तरह के हो सकते हैं। एक वे जो इस्लामी हुकूमत का ज़िम्मा क़बूल करते वक़्त कोई समझौता करें और दूसरे वे जो बग़ैर किसी समझौते के ज़िम्मा में दाख़िल हों। पहली क़िस्म के ज़िम्मियों के साथ तो वही मामला किया जाएगा जो समझौते में तय हुआ हो। रहे दूसरी क़िस्म के ज़िम्मी, तो उनका ज़िम्मी होना ही इस बात को लाज़िम करता है कि हम उनकी जान-माल और आबरू की उसी तरह हिफ़ाज़त करने के ज़िम्मेदार हैं जिस तरह ख़ुद अपनी जान-माल और आबरू की। उनके क़ानूनी हक़ वही होंगे जो मुसलमानों के होंगे। उनके ख़ून की क़ीमत वही होगी जो मुसलमान के ख़ून की है। उनको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी। उनकी इबादतगाहें (पूजा-स्थल) महफ़ूज़ रहेंगी, उनको अपनी मज़हबी तालीम का इन्तिज़ाम करने का अधिकार दिया जाएगा और इस्लामी तालीम उन पर ज़बरदस्ती नहीं ठूँसी जाएगी।
अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़िम्मियों के बारे में इस्लामी क़ानून की तफ़सील पर हम एक अलग किताब लिखेंगे। [इस विषय पर दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।]
(4) जहाँ तक ज़िम्मियों के 'पर्सनल लॉ' का ताल्लुक़ है तो वह उनकी मज़हबी आज़ादी का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए इस्लामी हुकूमत उनके शादी-विवाह और तलाक़ के क़ानून और विरासत, गोद लेने वग़ैरह के नियमों और ऐसे ही दूसरे तमाम क़ानूनों को, जो मुल्की क़ानून (Law of the Land) से न टकराते हों, उनपर जारी करेगी और सिर्फ़ उन बातों में उनके 'पर्सनल लॉ' को लागू करने को सहन न करेगी जिनका बुरा असर दूसरों पर पड़ता हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़िम्मी क़ौम सूद (ब्याज) को वैध समझती हो तो हम इसको इस्लामी हुकूमत में सूदी लेन-देन की इजाज़त न देंगे क्योंकि इससे पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ता है। या मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़िम्मी क़ौम ज़िना (व्यभिचार) को वैध समझती हो तो हम उसे इजाज़त न देंगे कि वह अपने तौर पर वेश्यावृत्ति (Prostitution) का कारोबार जारी रख सके क्योंकि इसे कोई भी इनसानी अख़्लाक़ तस्लीम नहीं करता और यह इनसानी अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ है और यह चीज़ हमारे आपराधिक क़ानून (Criminal Law) से भी टकराती है जो ज़ाहिर है मुल्की क़ानून भी होगा। इसी बुनियाद पर आप दूसरे हुक्मों और क़ानून के बारे में भी सोच सकते हैं।
(5) आपका यह सवाल कि क्या ज़िम्मी देश की शासन-व्यवस्था में बराबर के भागीदार हो सकते हैं? जैसे पुलिस, फ़ौज और क़ानून लागू करनेवाली संस्था में हिन्दुओं का हिस्सा होगा या नहीं? अगर नहीं तो क्या हिन्दुओं की अकसरियत वाले इलाक़ों में आप मुसलमानों के लिए वह हैसियत तस्लीम करेंगे जो आप हिन्दुओं को इस्लामी हुकूमत में देंगे? मेरी नज़र में यह सवाल दो ग़लत-फ़हमियों की बुनियाद पर है। एक यह कि उसूली ग़ैर-क़ौमी हुकूमत (Ideological Non-National State) की हैसियत आपने इसमें अपनी नज़र के सामने नहीं रखी है, दूसरे यह कि कारोबारी लेन-देन की ज़हनियत इसमें झलकती हुई महसूस होती है।
जैसा कि मैं नम्बर एक में वाज़ेह कर चुका हूँ कि उसूली हुकूमत को चलाने और उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वही लोग उठा सकते हैं जो उस उसूल पर यक़ीन रखते हों और वही उसकी रूह को समझ सकते हैं। उन्हीं से यह आशा की जा सकती है कि पूरे ख़ुलूस के साथ अपना दीन-ईमान समझते हुए उस हुकूमत के काम को चलाएँगे। और उन्हीं से यह उम्मीद की जा सकती है कि उस देश की हिमायत के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो जंग के मैदान में क़ुरबानी दे सकेंगे। दूसरे लोग जो उस उसूल पर ईमान नहीं रखते अगर हुकूमत में शरीक किए भी जाएँगे तो न वे उसकी उसूली और अख़लाक़ी रूह (नैतिक आत्मा) को समझ सकेंगे, न उस रूह के मुताबिक़ काम कर सकेंगे और न उनके अन्दर उन नियमों के लिए ख़ुलूस और निष्ठा का भाव होगा जिन पर उस हुकूमत की इमारत खड़ी होगी। सरकारी विभागों में अगर वे काम करेंगे तो उनके अन्दर नौकरी की ज़हनियत काम कर रही होगी और केवल रोज़गार ही के लिए वे अपना वक़्त और क़ाबलियतें बेचेंगे। अगर वे लोग फ़ौज में जाएँगे तो उनकी हैसियत किराए के सिपाहियों (Mercenaries) जैसी होगी और वे उन अख़्लाक़ी (नैतिक) माँगों को पूरा न कर सकेंगे जो इस्लामी हुकूमत अपने सैनिकों से करती है। इसलिए उसूली तौर पर और अख़्लाक़ी लिहाज़ से इस्लामी हुकूमत की पोज़ीशन इस मामले में यह है कि वह फ़ौज में ज़िम्मी लोगों से कोई ख़िदमत नहीं लेती बल्कि इसके ख़िलाफ़ फ़ौजी हिफ़ाज़त का पूरा बोझ मुसलमानों पर डाल देती है और ज़िम्मी लोगों से उनकी हिफ़ाज़त करने का उनसे सिर्फ़ एक टैक्स (Defencive Tax) लेकर फ़ौजी ज़िम्मेदारियों से उन्हें आज़ाद रखती है। यह टैक्स और फ़ौजी ख़िदमत दोनों एक साथ ज़िम्मी लोगों से नहीं लिए जा सकते।
अगर ज़िम्मी लोग अपने आपको ख़ुद फ़ौजी ख़िदमत के लिए पेश करें तो वह उनसे क़बूल कर ली जाएगी और इस सूरत में उनसे उनकी हिफ़ाज़त करने का टैक्स नहीं लिया जाएगा। रहे आम सरकारी विभाग तो उनके कलीदी मनसबों (Key Positions) और वे ख़ास ओहदे जो पॉलिसी बनाने के लिए होते हैं, किसी भी हालत में ज़िम्मी लोगों को नहीं दिए जा सकते। अलबत्ता कार्यकर्ताओं की हैसियत से ज़िम्मियों की सेवाएँ लेने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह जो एसेम्बली शूरा (सलाहकार समिति) के लिए चुनी जाएगी उसमें भी ज़िम्मियों को सदस्यता या राय देने का हक़ नहीं मिलेगा। लेकिन ज़िम्मियों की अलग कौंसिलें बना दी जाएँगी जो उनके तहज़ीब से ताल्लुक़ रखनेवाले इख़्तियारों की देख-भाल भी करेंगी और इसके अलावा हुकूमत के इन्तिज़ाम और बंदोबस्त के बारे में अपनी ख़्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें, अपनी शिकायतें और अपनी तज्वीज़ें भी पेश कर सकेंगी। जिनका पूरा-पूरा लिहाज़ इस्लामी मजलिसे-शूरा (Assembly) करेगी।
साफ़ और सीधी बात यह है कि इस्लामी हुकूमत किसी क़ौम का इजारा (ठेका) नहीं है, जो भी उसके उसूलों को क़बूल करे वह उस हुकूमत को चलाने में भागीदार हो सकता है चाहे वह हिन्दू हो या सिख, लेकिन जो उसके उसूलों को क़बूल न करे, न माने वह चाहे मुस्लिम की औलाद ही क्यों न हो, हुकूमत की सुरक्षा (Protection) से तो फ़ायदा उठा सकता है लेकिन उसके चलाने में हिस्सेदार नहीं हो सकता।
आपका यह सवाल कि “क्या तुम हिन्दू अकसरियत वाले सूबों (इलाक़ों) में मुसलमानों की वही पोज़ीशन क़बूल करोगे जो इस्लामी हुकूमत में हिन्दुओं को दोगे?" अस्ल में मुस्लिम लीग के लीडरों से किया जाना चाहिए था। क्योंकि लेने-देन की बातें वही कर सकते हैं। हमसे आप पूछेंगे तो हम तो इसका बेलाग उसूली जवाब देंगे।
जहाँ पर हुकूमत क़ायम करने के इख़्तियार हिन्दुओं को हासिल हों वहाँ आप उसूली तौर पर दो ही तरह की हुकूमतें क़ायम कर सकते हैं।
• ऐसी हुकूमत जो हिन्दू मज़हब की बुनियाद पर क़ायम हो।
• या फिर ऐसी हुकूमत जो वतनी क़ौमियत (राष्ट्रवाद) की बुनियाद पर क़ायम हो।
पहली हालत में आपके लिए यह कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि जैसे अधिकार इस्लामी हुकूमत में हिन्दुओं को मिलेंगे वैसे ही हुक़ूक़ (अधिकार) हम “राम-राज्य" में मुसलमानों को देंगे, बल्कि आपको इस मामले में कोई रहनुमाई हिन्दू धर्म में मिलती है तो पूरी तरह उसी पर अमल करें, इस बात की परवाह किए बग़ैर कि दूसरे किस तरह अमल करते हैं। अगर आपका मामला हमारे मामले से बेहतर होगा तो अख़्लाक़ (नैतिकता) के मैदान में आप हमपर फ़तह पाएँगे, और दूर नहीं कि एक दिन हमारी इस्लामी हुकूमत आपके राम-राज्य में तबदील हो जाए और अगर मामला इसके ख़िलाफ़ हुआ तो ज़ाहिर है कि देर या सवेर नतीजा भी ख़िलाफ़ ही निकलकर रहेगा।
रही दूसरी सूरत कि आपकी हुकूमत वतनी क़ौमियत की बुनियाद पर क़ायम हो तो इस सूरत में भी आपके लिए इसके सिवा चारा नहीं कि या तो लोकतान्त्रिक (Democratic) उसूल अपनाएँ और मुसलमानों को उनकी तादाद के लिहाज़ से हिस्सा दें। या फिर साफ़-साफ़ कह दें कि यह तो हिन्दू क़ौम की हुकूमत है और मुसलमानों को इसमें एक अधीन रहनेवाली क़ौम (Subject Nation) की हैसियत से रहना होगा।
इन दोनों सूरतों में से जिस सूरत पर भी आप चाहें मुसलमानों से मामला करें, किसी हाल में आपके बरताव को देखकर इस्लामी हुकूमत उन उसूलों में ज़र्रा बराबर भी कोई बदलाव न करेगी जो ज़िम्मियों से मामला करने के लिए क़ुरआन और हदीस में मुक़र्रर कर दिए गए हैं। आप चाहें तो अपनी क़ौमी हुकूमत में मुसलमानों को क़त्ल कर दें और एक मुसलमान बच्चे तक को ज़िन्दा न छोड़ें, इस्लामी हुकूमत में इसका बदला लेने के लिए किसी ज़िम्मी का बाल बाँका तक न किया जाएगा, इसके ख़िलाफ़ आपका जी चाहे तो हिन्दू हुकूमत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कमांडर इन चीफ़ सभी कुछ मुसलमान बाशिन्दों ही को बना दें। बहरहाल इसके जवाब में कोई एक ज़िम्मी भी किसी ऐसी पोज़ीशन पर मुक़र्रर नहीं किया जाएगा जो इस्लामी रियासत की पॉलिसी की शक्ल और दिशा तय करने में दख़ल रखती हो।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जुलाई-अक्टूबर 1944 ई.)
एक और स्पष्टीकरण
सवाल
आपकी तमाम किताबों और पिछले ख़तों को पढ़ने के बाद मैं यह फ़ैसला लेने पर अपने आप को सही समझता हूँ कि आप ख़ालिस इस्लामी ढंग की हुकूमत क़ायम करने के ख़ाहिशमन्द हैं और उस इस्लामी हुकूमत के ज़माने में ज़िम्मी और अहले-किताब की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी हिन्दुओं में अछूतों की।
आपने लिखा है कि “हिन्दुओं की इबादतगाहें (पूजास्थल) सुरक्षित रहेंगी। उनको मज़हबी तालीम का इन्तिज़ाम करने का अधिकार दिया जाएगा।" मगर आपने यह नहीं लिखा कि क्या हिन्दुओं को अपने मज़हब के प्रचार का हक़ भी हासिल होगा या नहीं? आपने यह भी लिखा है कि “जो भी इस हुकूमत के उसूल (सिद्धांतों) को तस्लीम कर ले वह उसके चलाने में हिस्सेदार हो सकता है चाहे वह हिन्दू की औलाद हो या सिख की औलाद।” मेहरबानी करके इसको वाज़ेह (स्पष्ट) कीजिए कि एक हिन्दू हिन्दू रहते हुए भी क्या आपकी हुकूमत के उसूलों पर ईमान लाकर उसे चलाने में शरीक हो सकता है?
फिर आपने यह कहा कि अहले-किताब की औरतों से मुसलमान शादी कर सकते हैं, मगर आपने साथ ही यह स्पष्ट नहीं किया कि अहले-किताब भी मुस्लिम औरतों से निकाह कर सकते हैं या नहीं? अगर जवाब न में है तो क्या आप अपने को ऊँचा समझने के इस एहसास (Superiority Complex) के बारे में और ज़्यादा रौशनी डालेंगे? अगर आप इसको सही ठहराने (Justification) के लिए इस्लाम पर ईमान की आड़ लें तो क्या यह मानने के लिए तैयार हैं कि मौजूदा नाम-निहाद (तथाकथित) मुसलमान आपके क़ौल के मुताबिक़ उन इस्लामी क़ायदों और कैरेक्टर (चरित्रों) के उसूलों पर पूरे उतरेंगे? आज के मुसलमान की बात तो अलग रही, क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि ख़िलाफ़ते-राशिदा के दौर में अक्सर व बेशतर जो लोग इस्लाम लाए उनमें ज़्यादातर सियासी ओहदों के चाहनेवाले थे? अगर आप यह स्वीकार नहीं कर सकते तो बताइए कि वह इस्लामी हुकूमत क्यों सिर्फ़ तीस-पैंतीस साल चलकर रह गई? फिर क्यों हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसे सोच-विचार रखनेवाले और मुजाहिद की इतनी सख़्त मुख़ालिफ़त हुई और मुख़ालफ़ित करनेवालों में हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) तक थीं?
आप इस्लामी हुकूमत की चाहत रखते हुए भी पाकिस्तान का विरोध करते हैं। क्या आप अपनी इस्लामी हुकूमत मुल्की हदों के बग़ैर ही लागू कर सकेंगे। यक़ीनन नहीं। मुख़ालिफ़त हुई तो फिर आपकी इस्लामी हुकूमत के लिए मुल्की हदें (सीमाएँ) बहरहाल वही सही हो सकती हैं जहाँ मिस्टर जिन्ना और उनके सहयोगी पाकिस्तान के लिए जिद्दोजुहद कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की सीमाओं के अलावा क्यों सारे भारत में इस्लामी हुकूमत लागू करेंगे? और यह गिरह भी खोलिए कि मौजूदा माहौल में इस ढंग की हुकूमत को चलाने के लिए ऐसे बुलन्द अख़लाक़ (उच्च नैतिक आदर्श) और बेहतरीन कैरेक्टर वाली हस्तियाँ कहाँ से पैदा करेंगे? जबकि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसे बेमिसाल बुज़ुर्ग उसे कुछ सालों से ज़्यादा न चला सके। चौदह सौ साल के बाद ऐसे कौन-से मुवाफ़िक़ हालात आपके पेशेनज़र हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी दूररस निगाहें इस्लामी हुकूमत को अमली सूरत में देख रही हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आपका पैग़ाम हर ख़याल के मुसलमान में ज़ोर-शोर से फैल रहा है और मुझे जिस क़द्र भी मुसलमानों से मिलने का मौक़ा मिला है वे सब इस ख़याल को मानते हैं कि आपने जो कुछ कहा है ठीक वही इस्लाम है, मगर हर आदमी का सवाल वही है जो मैंने पिछली पंक्तियों में पेश किया है। यानी आपके पास ख़िलाफ़ते-राशिदा के दौर की उसूली हुकूमत चलाने के लिए इस ज़माने में उस कैरेक्टर के आदमी कहाँ हैं? फिर जब वे बेहतरीन नमूने की हस्तियाँ इस निज़ाम (व्यवस्था) को आधी सदी तक भी कामयाबी से न चला सकीं तो इस दौर में उस ढंग की हुकूमत का ख़याल ख़ुशफ़हमी के सिवा और क्या हो सकता है।
इसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मेरा यह ख़याल था कि सिर्फ़ हम हिन्दुओं में ही एक मुश्तरका नस्बुलऐन (संयुक्त उद्देश्य) नहीं है, इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों में इज्तिमाई ज़िंदगी (सुसंगठित जीवन) है और उनके सामने एक अकेला उद्देश्य (नस्बुलऐन) है लेकिन अब इस्लामी हुकूमत का गहरा मुताला (अध्ययन) करने पर मालूम हुआ कि वहाँ का हाल हम से भी गया गुज़रा है। आपसे छिपाऊँगा नहीं, मैंने तरह-तरह की फ़िक्र रखनेवाले तक़रीबन सभी मुस्लिम रहनुमाओं से उनके नस्बुलऐन (उद्देश्य) और काम करने के तरीक़े के बारे में हक़ के एक खोजी की हैसियत से कुछ एक बातें जो मेरे लिए जानना ज़रूरी थीं, पूछीं। उनके जवाब मिलने पर मेरा पहला ख़याल ग़लत निकला और मालूम हुआ कि मुसलमानों में भी काम करने के तरीक़े और नस्बुलऐन के बारे में ज़बरदस्त इख़्तिलाफ़ पाया जाता है।
(इस मौक़े पर पूछनेवाले ने जमाअते-इस्लमी से इख़्तिलाफ़ रखनेवाले कुछ लोगों की किताबों से कुछ लाइनें नक़ल की हैं उन्हें निकाल दिया गया है।)
इन ठोस हक़ीक़तों को अनदेखा करके सिर्फ़ किताबों के पन्नों पर एक चीज़ को नज़रिए की शक्ल में पेश कर देना और बात है और उसे अमली रूप दे देना बिल्कुल अलग चीज़। राजनीति एक ठोस हक़ीक़त है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्या आप मेरी इन सारी गुज़ारिशों को सामने रखकर अपने काम करने के ढंग और अमल को तफ़सील के साथ बताएँगे?
जवाब
आपके सवालों का सिरा हक़ीक़त में अभी तक मैं नहीं पा सका हूँ। इस वजह से जो जवाब मैं देता हूँ, उनमें से कुछ और ऐसे सवाल निकल आते हैं जिनके निकलने की मुझे उम्मीद नहीं होती। अगर आप पहले बुनियादी मामलों से बात शुरू करें और फिर आगे बढ़ते हुए ग़ैर बुनियादी मामलों और वक़्ती सियासतों (Current Politics) की तरफ़ आएँ तो चाहे आप मुझसे मुत्तफ़िक़ न हों लेकिन कम-से-कम मुझे अच्छी तरह समझ ज़रूर लेंगे। इस वक़्त तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी पोज़ीशन आपके सामने पूरी तरह वाज़ेह नहीं है।
आपने अपने ख़त में लिखा है कि “जिस इस्लामी हुकूमत का मैं ख़्वाब देख रहा हूँ उसमें ज़िम्मी (ग़ैर-मुस्लिम) और अहले-किताब की हैसियत वही होगी जो हिन्दुओं में अछूतों की है।" मुझे यह पढ़कर बहुत हैरत हुई कि या तो आप ज़िम्मियों की हैसियत मेरे साफ़-साफ़ बयान कर देने के बावजूद नहीं समझ पाए हैं या फिर हिन्दुओं में अछूतों की हैसियत क्या है, उसे आप जानते नहीं हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अछूतों की जो हैसियत मनु के धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) से मालूम होती है उसका उन अधिकारों और रिआयतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो अधिकार और रिआयतें इस्लामी क़ानून में ज़िम्मियों को दिए गए हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अछूतपन की बुनियाद नस्ली भेदभाव पर है और ज़िम्मियों की बुनियाद सिर्फ़ अक़ीदे (आस्था) पर। अगर ज़िम्मी इस्लाम क़बूल कर ले तो वह हमारा अमीर और इमाम (नायक) तक बन सकता है मगर एक शूद्र किसी अक़ीदे व मसलक को क़बूल कर लेने के बाद भी वर्णाश्रम की पाबन्दियों से छुटकारा नहीं पा सकता।
आपका यह सवाल बहुत ही अजीब है कि “क्या एक हिन्दू हिन्दू रहते हुए भी आपकी हुकूमत के उसूलों पर ईमान लाकर उसे चलाने में शरीक हो सकता है?" शायद आपने इस बात पर ग़ौर नहीं किया कि इस्लामी हुकूमत के उसूलों पर ईमान ले आने के बाद हिन्दू हिन्दू कब रहेगा। वह तो मुस्लिम हो जाएगा। आज जो करोड़ों “हिन्दुओं की औलादें" इस देश में मुसलमान हैं वे सब इस्लाम के उसूलों पर ईमान लाकर ही तो मुसलमान हुई हैं। इसी तरह आगे भी जो हिन्दुओं की औलादें उसे मान लेंगी वे भी मुस्लिम हो जाएँगी, और जब वे मुस्लिम हो जाएँगी तो यक़ीनन इस्लामी हुकूमत के चलाने में वे हमारे साथ बराबर की शरीक होंगी।
आपका यह सवाल कि “क्या हिन्दुओं को इस्लामी रियासत में अपने मज़हब के प्रचार का हक़ भी प्राप्त होगा या नहीं?" सवाल जितना छोटा है उसका जवाब उतना छोटा नहीं है। मज़हब के प्रचार की कई शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि कोई मज़हबी गरोह ख़ुद अपनी आनेवाली नस्लों को और अपने आम लोगों को अपने धर्म की शिक्षा दे, इसका हक़ तमाम ज़िम्मी-समाज को हासिल होगा। दूसरी शक्ल यह है कि कोई मज़हबी गरोह किताबों और तक़रीरों (भाषणों) के ज़रिये से अपने मज़हब को दूसरों के सामने पेश करे और इस्लाम समेत दूसरे मज़हबों से अपने इख़्तिलाफ़ की वजहों को इल्मी हैसियत से बयान करे, इसकी इजाज़त भी ज़िम्मियों को होगी।...... तीसरी शक्ल यह है कि कोई गरोह अपने धर्म की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म (सुसंगठित) तहरीक उठाए जिसका मक़सद या जिसका नतीजा यह हो कि मुल्क की ज़िन्दगी का निज़ाम बदल कर इस्लामी उसूलों के बजाय उसके उसूलों पर क़ायम हो जाए। ऐसे मज़हबी तब्लीग़ की इजाज़त इस्लामी राज्य की सीमाओं में किसी को हासिल न होगी।
अहले-किताब की औरतों से मुसलमान की शादी जाइज़ और मुसलमान औरतों से अहले-किताब की शादी नाजाइज़ होने की बुनियाद किसी एहसासे-बरतरी पर नहीं है, बल्कि यह एक नफ़सियाती (मनोवैज्ञानिक) हक़ीक़त पर आधारित है। मर्द आम तौर पर कम मुतास्सिर होता है और असर ज़्यादा डालता है और औरत मुतास्सिर ज़्यादा होती है और असर कम डालती है। एक ग़ैर-मुस्लिम औरत अगर किसी मुसलमान के निकाह में आए तो इसकी उम्मीद कम है कि वह उस मुसलमान को ग़ैर-मुस्लिम बना लेगी और इस बात का इमकान ज़्यादा है कि वह मुसलमान हो जाएगी। लेकिन एक मुसलमान औरत अगर किसी ग़ैर-मुस्लिम के निकाह में आए तो उसके ग़ैर-मुस्लिम बन जाने का अन्देशा ज़्यादा है और इस बात की उम्मीद कम है कि वह अपने शौहर को और अपनी औलाद को मुसलमान बना सकेगी। इसी लिए मुसलमानों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि वे अपनी लड़कियों का निकाह ग़ैर-मुस्लिमों से करें; अलबत्ता अगर अहले-किताब में से कोई आदमी अपनी बेटी मुसलमान को देने पर राज़ी हो तो मुसलमान उससे निकाह कर सकता है। लेकिन क़ुरआन मजीद में जहाँ इस चीज़ की इजाज़त दी गई है वहाँ साथ ही यह धमकी भी दी गई है कि अगर ग़ैर-मुस्लिम बीवी की मुहब्बत में पड़कर तुमने ईमान खो दिया तो तुम्हारा सब किया कराया बरबाद हो जाएगा और आख़िरत में तुम घाटे में रहोगे। यह इजाज़त ऐसी है जिससे ख़ास ज़रूरतों के मौक़ों पर ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। यह कोई पसन्दीदा अमल नहीं है जिसे आम मक़बूलियत हासिल हो बल्कि कुछ हालतों में तो इससे रोका भी गया है ताकि मुसलमानों की सोसाइटी पाक-साफ़ रहे और उसमें कोई अख़्लाक़ी और अक़ीदे से मुताल्लिक़ कोई बुराई न पल-बढ़ पाए।
आपका यह सवाल कि इस्लामी हुकूमत सिर्फ़ तीस-पैंतीस साल चलकर क्यों रह गई, एक अहम तारीख़ी (ऐतिहासिक) मसले से मुताल्लिक़ है। अगर आप इस्लामी इतिहास का गहरा अध्ययन करें तो उसके कारणों को समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल न होगा। किसी ख़ास उसूल की अलम्बरदार जमाअत जो ज़िन्दगी का निज़ाम क़ायम करती है उसका अपनी पूरी शान के साथ चलना और क़ायम रहना इस बात पर निर्भर होता है कि लीडरशिप (नेतृत्व) एक ऐसे चुने हुए गरोह के हाथ में रहे जो उस उसूल का सच्चा और सरगर्म अनुयायी हो और लीडरशिप ऐसे गरोह के हाथ में सिर्फ़ उसी हालत में रह सकती है जबकि आम बाशिन्दों पर उस गरोह की पकड़ बनी रहे और उनकी बहुत बड़ी तादाद कम-से-कम इस हद तक तालीम व तरबियत पाए हुए हो कि उसे उस ख़ास उसूल के साथ गहरा लगाव भी हो और वह उन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार भी न हो जो उस उसूल से हटकर किसी दूसरे तरीक़े की तरफ़ बुलानेवाले हों। यह बात अच्छी तरह मन में बिठा लेने के बाद इस्लामी इतिहास पर नज़र डालिए।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में जो तहज़ीबी (सांस्कृतिक) इंक़िलाब (Cultural Revolution) पैदा हुआ, जो नई जीवन-व्यवस्था क़ायम हुई, उसकी बुनियाद यह थी कि अरब की आबादी में एक तरह का अख़्लाक़ी इंक़िलाब (Moral Revolution) पैदा हो चुका था और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क़ियादत (नेतृत्व) में जो सच्चे और नेक इनसानों का छोटा गरोह तैयार हुआ था उसकी क़ियादत को तमाम अरबवालों ने तस्लीम कर लिया था। लेकिन आगे चलकर ख़िलाफ़ते-राशिदा के ज़माने में जब मुल्क पर मुल्क फ़तह होने शुरू हुए तो इस्लामी हुकूमत में विस्तार और फैलाव बहुत तेज़ी के साथ होने लगा, लेकिन इस्तिहकाम (स्थायित्व) उतना तेज़ी के साथ न हो सका। चूँकि उस ज़माने में प्रचार-प्रसार और तालीम व तबलीग़ के साधन इतने न थे जितने आज हैं और न आने-जाने के साधन मौजूदा ज़माने की तरह थे, इसलिए जो फ़ौज-दर-फ़ौज इनसान उस नई मुस्लिम सोसाइटी में दाख़िल होने शुरू हुए उनको अख़लाक़ी, ज़ेहनी और अमली हैसियत से इस्लामी तहरीक में पूरे तौर पर घुलाने-मिलाने का इन्तिज़ाम न हो सका। नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों की आम आबादी में सही क़िस्म के मुसलमानों का तनासुब (अनुपात) बहुत कम रह गया और कच्चे क़िस्म के मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन उसूली तौर पर उन मुसलमानों के हुक़ूक़ और अधिकार और सोसाइटी में उनकी हैसियत सही क़िस्म के मुसलमानों के मुक़ाबले में कुछ भी अलग न हो सकती थी, इसी वजह से जब हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में इर्तिजाई तहरीकें (Reactionary Movements) [यानी जिनका मक़सद इस्लाम से फिर कर किसी न किसी तरह जाहिलियत की तरफ़ पलट जाना था।] पैदा हुईं तो आम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे प्रभावित हो गया और लीडरशिप उन लोगों के हाथों से निकल गई जो ठेठ इस्लामी ढंग पर काम करनेवाले थे। इस ऐतिहासिक हक़ीक़त को समझ लेने के बाद हमें यह वाक़िआ ज़र्रा बराबर भी निराश नहीं करता कि ख़ालिस इस्लामी हुकूमत तीस-पैंतीस साल से ज़्यादा मुद्दत तक क़ायम न रह सकी।
आज अगर हम एक नेक गरोह उस ज़ेहनियत, उस अख़्लाक़ और उस चरित्र के इनसानों को एकजुट कर सकें जो इस्लाम के मंशा के मुताबिक़ हो, तो हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा ज़माने के साधनों से फ़ायदा उठाकर न सिर्फ़ अपने देश बल्कि संसार के दूसरे देशों में भी हम एक अख़्लाक़ी और तमद्दुनी इन्क़िलाब बरपा कर सकेंगे और हमें पूरा यक़ीन है कि ऐसे गरोह के संगठित हो जाने के बाद आम इनसानों की क़ियादत और बागडोर उस गरोह के सिवा किसी दूसरी पार्टी के हाथों में नहीं जा सकती। आप मुसलमानों की मौजूदा हालत को देखकर जो राय क़ायम कर रहे हैं वह उस हालत पर फ़िट नहीं हो सकती जो हमारी नज़र के सामने है।
अगर सही अख़्लाक़ के इनसान अमली मैदान में आ जाएँ तो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि मुसलमान जनता ही नहीं बल्कि हिन्दू, ईसाई, पारसी, सिख और दूसरी क़ौमें सब उनको दिल से चाहने लगेंगे और ख़ुद अपने मज़हब के लीडरों को छोड़कर उन पर भरोसा करने लगेंगे। ऐसे ही एक गरोह को तरबियत और तालीम और संगठन के ज़रिये से तैयार करना मेरा मक़सद है और मैं ख़ुदा से दुआ करता हूँ कि इस काम में वह मेरी मदद करे।
इस्लामी हुकूमत' और 'पाकिस्तान' के फ़र्क़ के बारे में जो सवाल आपने किया है उसका जवाब आप मेरी किताबों में पा सकते थे। मगर शायद वे आपकी नज़र से नहीं गुज़रीं। पाकिस्तान की माँग की बुनियाद क़ौमियत के उसूल पर है यानी मुसलमान क़ौम के लोग जहाँ अकसरीयत में हों वहाँ उन्हें अपनी हुकूमत क़ायम करने का हक़ हासिल हो। इसके ख़िलाफ़ इस्लामी हुकूमत की तहरीक की बुनियाद इस्लाम का उसूल है। पाकिस्तान सिर्फ़ उन लोगों को अपील कर सकता है जो मुसलमान क़ौम से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस्लामी हुकूमत की दावत तमाम इनसानों को अपील कर सकती है। चाहे वे पैदाइशी मुसलमान हों या पैदाइशी हिन्दू या कोई और। पाकिस्तान सिर्फ़ वहीं क़ायम हो सकता है जहाँ मुसलमानों की अकसरीयत है और इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि इस तहरीक के नतीजे में एक ख़ालिस इस्लामी हुकूमत क़ायम होगी। क्योंकि ख़ालिस इस्लामी हुकूमत का क़ायम होना जिस अख़्लाक़ी इन्क़िलाब पर निर्भर है वह पाकिस्तान के आन्दोलन से पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की हुकूमत इसकी मुहताज नहीं है कि किसी जगह मुसलमान क़ौम ज़्यादा तादाद में पहले से मौजूद हो। वह तो एक अख़्लाक़ी, ज़ेहनी, तमद्दुनी (सांस्कृतिक) इन्किलाब की दावत है और सारे इनसानों के लिए ख़ुद उन्हीं की भलाई और कामयाबी के कुछ उसूल पेश करती है। इस दावत को अगर पंजाब या सिन्ध सबसे पहले आगे बढ़कर क़बूल कर लें तो हुकूमत यहाँ क़ायम हो सकती है और अगर मद्रास (चेन्नई), मुम्बई या कोई दूसरा इलाक़ा आगे बढ़कर इसे क़बूल कर ले तो इस्लामी हुकूमत वहाँ क़ायम हो सकती है। हम इस दावत को मुसलमान, हिन्दू, सिख, ईसाई हर एक के सामने पेश करते हैं। हमारे नज़दीक यह मुसलमानों की कोई क़ौमी जायदाद नहीं है, बल्कि तमाम इनसानों की भलाई और कामयाबी के कुछ उसूल हैं। हो सकता है कि पैदाइशी मुसलमान इस दावत को क़बूल करने में कोताही दिखाएँ और पैदाइशी हिन्दू आगे बढ़कर एसे क़बूल कर लें।
आपका यह ख़याल बिल्कुल सही है कि मुसलमानों में मुश्तरका (संयुक्त) मक़सद और नस्बुलऐन (लक्ष्य) की कमी हिन्दुओं से भी कहीं ज़्यादा पाई जाती है। हक़ीक़त में यह सब कुछ नतीजा है इस्लाम से बेपरवाह हो कर दुनियावी मामलों को मन-मर्ज़ी और ग़ैर इस्लामी तौर-तरीक़ों की तक़लीद (अनुसरण) से हल करने की कोशिश का। अगर मुसलमान ख़ालिस इस्लामी उसूल पर अपने और समाज से जुड़े मामलों को हल करने की कोशिश करते तो आप उनको एक ही मक़सद और एक ही नस्बुलऐन के पीछे अपनी सारी ताक़तें ख़र्च करते हुए पाते। आपने मुसलमानों के अन्दर ख़याल और अमल का जो बिखराव और बिगाड़ महसूस किया है उसे मैं भी एक मुद्दत से देख रहा हूँ और हमारी इस्लामी तहरीक के साथ मुसलमानों के मुख़्तलिफ़ तबक़ों का जो बर्ताव है वह भी मेरी निगाह में है। मगर इन चीज़ों से मेरे अन्दर कोई बददिली पैदा नहीं होती क्योंकि इन बातों की तह में जो अस्ल ख़राबी है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। सिर्फ़ यही नहीं कि मैं बददिल नहीं हूँ बल्कि एक बड़ी हद तक उम्मीदों से भरा हुआ भी हूँ जैसा कि आपने ख़ुद भी लिखा है। मुसलमानों का पढ़ा-लिखा तबक़ा बड़ी तेज़ी के साथ इस बात को तस्लीम करता जा रहा है कि जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ वही अस्ल और ख़ालिस इस्लाम है। इसके साथ मैं यह भी देख रहा हूँ कि मुसलमानों के मौजूदा मुख़्तलिफ़ गरोह जिस ढंग पर काम कर रहे हैं उससे उनका कामयाबी की मंज़िल तक पहुँचना तक़रीबन नामुमकिन (असम्भव) है। लिहाज़ा इस बात की पूरी उम्मीद है कि आनेवाले ज़माने में जल्द ही मुसलमान नौजवान इन मुख़्तलिफ़ गरोहों से और उनकी राजनीति से मायूस हो जाएँगे और उनके लिए ख़ालिस इस्लाम के उसूलों पर काम करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि मैं तो यह देख रहा हूँ कि हिन्दुओं में भी जब क़ौमपरस्ती सियासी आज़ादी की मंज़िल पर पहुँच जाएगी तो उन्हें राजनीति, समाज और तमद्दुन की मशीनरी को चलाने के लिए कुछ उसूल दरकार होंगे और वे उसूल गाँधी जी के फ़लसफ़े (दर्शन) में या काँग्रेस की वतन-परस्ती और हिन्दू महासभा की क़ौम-परस्ती में न मिल सकेंगे। उस वक़्त उनके लिए सिर्फ़ दो ही रास्ते होंगे, या तो कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) के उसूलों को अपनाएँ या फिर इस्लाम के उसूलों को क़बूल कर लें। उस मौक़े के पेश आने तक अगर हम बिना लाग-लपेट के इस्लामी उसूल की ओर दावत देनेवालों का एक नेक और सच्चा गरोह बनाने में कामयाब हो गए तो मुझे अस्सी फ़ीसदी (80%) उम्मीद है कि हम अपने हिन्दू और सिख भाइयों को कम्यूनिज़्म से बचाने और इस्लाम के उसूलों की तरफ़ खींच लाने में कामयाब हो जाएँगे।
हमारे इस मक़सद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानों और हिन्दुओं की मौजूदा क़ौमी कश-मकश (जातीय संघर्ष) है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीक़े पर हम काम कर रहे हैं उससे हम हिन्दुओं, सिखों और दूसरी ग़ैर-मुस्लिम क़ौमों के उस तास्सुब (पक्षपात) को जो वे इस्लाम के ख़िलाफ़ रखते हैं, आख़िरकार दूर कर देंगे। हम उन्हें इस बात पर आमादा कर लेंगे कि वे इस्लाम को ख़ालिस उसूली हैसियत से देखें, न कि उस क़ौम के मज़हब की हैसियत से जिसके साथ दुनियावी फ़ायदों के लिए उनकी मुद्दतों से कश-मकश चल रही है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, नवम्बर-दिसम्बर 1944 ई.)
इस्लाम में हाथ काटने की सज़ा
सवाल
इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ का काट देना है। आजकल रोज़ाना सैकड़ों चोरियाँ होती हैं तो क्या रोज़ाना सैकड़ों हाथ काटे जाएँगे? ज़ाहिरी हालात में यह सज़ा सख़्त और नाक़ाबिले-अमल मालूम होती है।
जवाब
हाथ काटने और इस्लाम के दूसरे फ़ौजदारी क़ानून के बारे में अगर मैं इस्लाम का नज़रिया पूरी तफ़सील के साथ बयान करूँ तो इसमें बहुत वक़्त लगेगा। मैं इस विषय पर अपनी किताब 'इस्लामी क़वानीन और पाकिस्तान में उसके नफ़ाज़ की अमली तदाबीर' में तफ़सील से बहस कर चुका हूँ। इस वक़्त मैं सिर्फ़ इतनी बात कहूँगा कि जब चोर के हाथ काटने का तरीक़ा जारी होगा तो अल्लाह ने चाहा तो चोरी बहुत ही थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी और सैकड़ों हाथों के कटने की नौबत नहीं आएगी। एक चोर यह उम्मीद रखता है कि मैं दस हज़ार रुपये चुरा लूँगा, अगर पकड़ा जाऊँगा तो कुछ मुद्दत तक सरकार की रोटियाँ खाकर वापस आ जाऊँगा, और उस वक़्त भी मेरे पास अच्छी ख़ासी दौलत जमा होगी। ज़ाहिर है कि ऐसा आदमी दोबारा मौक़ा पाते ही चोरी करेगा। इस तरह के आदी मुजरिमों की हमारे यहाँ बहुतात है और इन्हीं को जुर्म करने से बाज़ रखना इंतिहाई मुश्किल मसला है। लेकिन अगर चोर को यह मालूम हो कि एक बार पकड़े जाने के बाद एक हाथ और दूसरी मरतबा पकड़े जाने के बाद दूसरा हाथ कट जाएगा तो वह चोरी करने पर आसानी से तैयार न होगा। फिर जिस चोर का हाथ एक बार कट जाएगा वह जहाँ कहीं जाएगा उसका कटा हुआ हाथ पुकार-पुकारकर उसकी दास्तान बयान करेगा और मौजूदा सूरते-हाल बाक़ी नहीं रहेगी, जिसमें ये पेशेवर चोर और डाकू मुहज़्ज़ब (सभ्य) इनसानों के भेस में चारों तरफ़ अपना शिकार तलाश करते फिरते हैं और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता। मेरी दो टूक राय यह है कि चोरी रोकने के लिए इस क़ानून को लागू करने की बहुत ही सख़्त ज़रूरत है। आज की बहुत-सी ख़राबियों में से एक ख़राबी यह भी है कि उसकी सारी हमदर्दियाँ मुजरिम के साथ हैं, उस सोसाइटी के साथ नहीं हैं जिसके ख़िलाफ़ मुजरिम जुर्म करने में लगा हुआ है। सिर्फ़ यह सुनने पर कि चोर का हाथ काटा जाएगा इस तहज़ीब की औलादों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये दिल दहला देनेवाले जुर्मों को समाज में परवान चढ़ते देखकर टस-से-मस नहीं होते। आख़िर में यह वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि इस्लाम सिर्फ़ चोर का हाथ नहीं काटता बल्कि वह सदक़े (दान) और ज़कात का निज़ाम भी क़ायम करता है। हर आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। वह शहर के लोगों की अख़लाक़ी तालीम व तरबियत का भी इन्तिज़ाम करता है, वह लोगों को हलाल और जाइज़ तरीक़े से कमाना और ख़र्च करना भी सिखाता है। इसके बाद भी अगर कोई शख़्स किसी शख़्स की हलाल कमाई चुराता है तो चोर के हाथ काटने की सज़ा दी जाती है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, सितम्बर 1954 ई.)
बर्थ-कंट्रोल
सवाल
आजकल बर्थ-कंट्रोल को 'फ़ैमिली प्लानिंग' के नए उन्वान के तहत लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके हक़ में आर्थिक दलीलों के अलावा कुछ लोगों की तरफ़ से मज़हबी दलीलें भी दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि हदीस में अज़्ल (सम्भोग के समय वीर्य अन्दर के बजाय बाहर निकालने) की अनुमति है और बर्थ-कंट्रोल को इसी के जैसा समझा जा सकता है। इसके अलावा अब हुकूमत की तरफ़ से मर्दों को बाँझ बनाने की सहूलतें भी पैदा की जा रही हैं। अब तो कुछ ऐसे टीके भी बनाए जा रहे हैं जिनसे मर्द का हयाती जौहर यानी वीर्य इस क़ाबिल नहीं रहता कि वह नस्ल को बढ़ाने का ज़रीआ बन सके, लेकिन सेक्स का मज़ा बना रहता है। कुछ लोगों के नज़दीक यह तरीक़ा भी शरई तौर पर हराम नहीं। और न यह औलाद के क़त्ल या गर्भपात ही की श्रेणी में आ सकता है।
मेहरबानी करके इस बारे में बताएँ कि आपके नज़दीक इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है या नहीं?
जवाब
बर्थ-कंट्रोल के इस विषय पर मैं अब से कई साल पहले एक किताब 'इस्लाम और बर्थ-कंट्रोल' लिख चुका हूँ; जिसमें दीनी, मआशी (अर्थिक) और सामाजिक दृष्टिकोण से इस मसले के सारे पहलुओं पर बहस मौजूद है। अब इसका नया एडीशन भी छप चुका है। आपके सवाल का मुख़्तसर जवाब यह है कि 'अज़्ल' के बारे में जो कुछ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया और उसके जवाब में जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान फ़रमाया उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक आदमी की ज़रूरत और छूटवाली हालत से था। बर्थ-कंट्रोल की कोई आम दावत व तहरीक हरगिज़ पेशे-नज़र न थी। न ऐसी किसी तहरीक का कोई ख़ास फ़लसफ़ा (दर्शन) था जो लोगों में फैलाया जा रहा हो, न ऐसी तदबीरें बड़े पैमाने पर हर मर्द और औरत को बताई जा रही थीं कि वे आपस में सेक्स करने के बावुजूद हमल (गर्भ) के ठहरने को रोक सकें, और न हमल को रोकनेवाली दवाएँ और चीज़ें हर मर्द और औरत तक पहुँचाई जा रही थीं। 'अज़्ल' की अनुमति में जो कुछ रिवायतें बयान हुई हैं उनकी हक़ीक़त बस यह है कि अल्लाह के किसी बन्दे ने अपने हालात या मजबूरियाँ बयान कीं और प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें सामने रखकर कोई मुनासिब जवाब दे दिया। इस तरह के जो जवाब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से हदीस में बयान हुए हैं उनसे अगर 'अज़्ल' के जाइज़ होने की बात निकलती भी है तो वह हरगिज़ बर्थ-कंट्रोल की इस आम-सी तहरीक के हक़ में इस्तेमाल नहीं की जा सकती जिसके पीछे एक बाक़ायदा ख़ालिस दुनियापरस्ती और हर चीज़ को जाइज़ करने का फ़लसफ़ा काम कर रहा है। ऐसी कोई तहरीक अगर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने उठती तो मुझे यक़ीन है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसपर लानत भेजते और उसके ख़िलाफ़ वैसा ही जिहाद करते जैसा शिर्क और बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) के ख़िलाफ़ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किया। जो शख़्स भी 'अज़्ल' के बारे में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बयानों का ग़लत इस्तेमाल करके उन्हें मौजूदा तहरीक के हक़ में दलील के तौर पर पेश करता है, मैं उसे ख़ुदा से डराता हूँ और मशविरा देता हूँ कि वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुक़ाबले में इस जसारत (दुस्साहस) से बाज़ रहे। पश्चिम की बेख़ुदा तहज़ीब और फ़िक्र की पैरवी अगर किसी को करनी हो तो सीधी तरह उसे पश्चिमी दीन समझकर ही अपनाए। आख़िर वह इसे ख़ुदा और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही की तालीम क़रार देकर ख़ुदा का और ज़्यादा ग़ज़ब मोल लेने की कोशिश क्यों करता है?
इस्लाम जिस तरह बर्थ-कंट्रोल की आम तहरीक को जाइज़ नहीं मानता, उसी तरह वह जानबूझ कर बाँझ बनने की इजाज़त भी नहीं देता। यह कहना कि जानबूझकर अपने-आप को बाँझ कर लेना कोई नाजाइज़ काम नहीं है, उतना ही ग़लत है जितना यह कहना कि आदमी का ख़ुदकुशी कर लेना जाइज़ है। अस्ल में इस तरह की बातें वे लोग करते हैं जिनके नज़दीक आदमी अपने शरीर और उसकी ताक़तों का ख़ुद मालिक है और अपने शरीर और उसकी ताक़तों के साथ जो कुछ भी करना चाहे कर लेने का हक़ रखता है। इसी ग़लत ख़याल की वजह से जापानी ख़ुदकुशी को जाइज़ समझते हैं, इसी ग़लत ख़याल की वजह से कुछ जोगी अपने हाथ-पाँव या ज़बान (जीभ) बेकार कर लेते हैं। लेकिन जो आदमी अपने आपको ख़ुदा का ग़ुलाम या दास समझता हो और यह समझता हो कि यह शरीर और इसकी ताक़तें ख़ुदा की देन और उसकी अमानत हैं, उसके नज़दीक अपने आपको बाँझ कर लेना वैसा ही गुनाह है, जैसा कि किसी दूसरे इनसान को ज़बरदस्ती बाँझ कर देना या किसी की आँखों की रौशनी बरबाद कर देना गुनाह है।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, अप्रैल 1960 ई.)
बर्थ-कंट्रोल और नेत्र-दान
सवाल
दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए इस्लाम आज क्या हल पेश करता है? बर्थ-कंट्रोल के लिए दवाओं का इस्तेमाल, फ़ैमिली प्लानिंग (परिवार नियोजन) वग़ैरह को क्या आज भी ग़ैर शरई ठहराकर हराम क़रार दिया जाएगा? क्या एक मुसलमान ज़िन्दगी में अपनी आँखें दान कर सकता है कि मौत के बाद किसी मरीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकें? क्या यह क़ुरबानी या दान गुनाह तो न होगा और क़ियामत (परलोक) में वह व्यक्ति अन्धा तो न उठेगा?
जवाब
दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए इस्लाम सिर्फ़ एक ही हल पेश करता है, और वह यह कि अल्लाह ने रोज़ी के जो साधन पैदा किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए और जो साधन अब तक छिपे हुए हैं उनको खोज निकालने की कोशिश की जाती रहे। आबादी रोकने की हर कोशिश, चाहे वह औलाद का क़त्ल हो या हमल गिराना या हमल न ठहरने देना, ग़लत और बेहद तबाह करनेवाली है। बर्थ-कंट्रोल की तहरीक के चार नतीजे ऐसे हैं जिनको ज़ाहिर होने से किसी-तरह नहीं रोका जा सकता—
(1) ज़िना (व्यभिचार) का ज़्यादा होना।
(2) इनसान के अन्दर ख़ुदग़र्जी और अपनी ज़िंदगी का मेयार बढ़ाने की ख़ाहिश का इस हद तक बढ़ जाना कि उसे अपने बूढ़े माँ-बाप और अपने यतीम भाइयों और अपने दूसरे मदद के मुहताज रिश्तेदारों का वुजूद भी नागवार गुज़रने लगे। क्योंकि जो आदमी अपनी रोटी में ख़ुद अपनी औलाद को शामिल करने के लिए तैयार न हो वह दूसरों को भला कैसे शामिल कर सकेगा?
(3) आबादी के बढ़ने की कम से कम ज़रूरी तादाद भी जो एक क़ौम को ज़िन्दा रखने के लिए हर हाल में ज़रूरी है, बरक़रार न रहना। इसलिए कि जब यह फ़ैसला करनेवाले ख़ुद लोग होंगे कि वे कितने बच्चे पैदा करें और कितने न करें और इस फैसले का दारोमदार इस बात पर होगा कि वे अपनी ज़िंदगी के मेयार को नए बच्चों के आने की वजह से गिरने न दें तो आख़िरकार वे इतने बच्चे भी पैदा करने के लिए तैयार न होंगे जितने एक क़ौम को अपनी क़ौमी आबादी बरक़रार रखने के लिए दरकार होते हैं। इस तरह के हालात में कभी-कभी नौबत यह भी आ जाती है कि पैदाइश की दर मौत की दर से कमतर हो जाती है। चुनांचे यह नतीजा फ्रांस देख चुका है, यहाँ तक कि उसको “बच्चे ज़्यादा पैदा करो" की तहरीक चलानी पड़ी और इनाम देकर इसकी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ गई।
(4) क़ौमी दिफ़ा (राष्ट्रीय सुरक्षा) का कमजोर हो जाना। यह नतीजा ख़ास तौर पर एक ऐसी क़ौम के लिए बेहद ख़तरनाक है जो अपने से कई गुना ज़्यादा दुश्मन आबादी में घिरी हुई है।
आँख के दान का मामला सिर्फ़ आँखों तक ही महदूद नहीं रहता। बहुत से दूसरे अंग भी मरीज़ों के काम आ सकते हैं और उनके दूसरे लाभकारी इस्तेमाल भी हो सकते हैं। यह दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो मुसलमान का क़ब्र में दफ़न होना मुश्किल हो जाएगा। उसका सारा जिस्म ही चन्दे में बँटकर रहेगा। इस्लामी नज़रिया (दृष्टिकोण) यह है कि कोई आदमी अपने शरीर का मालिक नहीं है। उसको यह अधिकार नहीं पहुँचता कि मरने से पहले अपने शरीर को बाँटने या चन्दे में देने की वसीयत कर दे। शरीर उस वक़्त तक उसके इस्तेमाल में है जब तक वह उस शरीर में ख़ुद रहता है, उसके निकल जाने के बाद शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं है कि इसके मामले में उसकी वसीयत लागू हो। इस्लामी अहकाम के मुताबिक़ यह ज़िन्दा इनसानों का फ़र्ज़ है कि उसका जिस्म एहतिराम के साथ दफ़न कर दें।
इस्लाम ने इनसानी लाश के एहतिराम का जो हुक्म दिया वह अस्ल में इनसानी जान के एहतिराम का ज़रूरी हिस्सा है। एक बार अगर इनसानी लाश का एहतिराम ख़त्म हो जाए तो बात सिर्फ़ इस हद तक महदूद न रहेगी कि मुर्दा इनसानों के कुछ काम में आनेवाले अंग ज़िन्दा इनसानों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने लगेंगे, बल्कि धीरे-धीरे इनसानी जिस्म की चर्बी से साबुन भी बनने लगेंगे (जैसे कि हक़ीक़त में दूसरे महायुद्ध ज़माने में जर्मनों ने बनाए थे), इनसानी खाल को उतार कर उसको दबाग़त देने (चमड़ा बनाने) की कोशिश की जाएगी ताकि उसके जूते या सूटकेस या मिनीपर्स बनाए जा सकें। (चुनांचे यह तजरबा भी कुछ सालों पहले चैन्नई की एक टेनरी कर चुकी है), इनसान की हड्डियों, आँतों और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करने की भी फ़िक्र की जाएगी। यहाँ तक कि इसके बाद एक बार इनसान फिर उस ख़ौफ़नाक दौर की तरफ़ पलट जाएगा जब आदमी आदमी का गोश्त खाता था। मैं नहीं समझता कि अगर एक मुर्दा इनसान के अंग निकालकर इलाज में इस्तेमाल करना जाइज़ क़रार दे दिया जाए तो फिर किस जगह हदबन्दी करके आप उसी जिस्म के दूसरे “फ़ायदेमंद" इस्तेमाल को रोक सकेंगे और किस दलील से इस बन्दिश को अक़्ल के मुताबिक़ होना साबित करेंगे।
(तर्जमानुल-क़ुरआन, जनवरी 1962 ई.)
गाय, आवागमन और गुरु ग्रन्थ साहिब
सवाल
नीचे लिखे मसलों के बारे में अपनी मालूमात की रौशनी में हक़ीक़त की तरफ़ रहनुमाई करें। (1) गाय का एहतिराम और उसकी पाकी जो हिन्दू भाइयों में राइज है उसकी वजह से सैकड़ों बार हिन्दू-मुस्लिम झगड़े-फ़साद हो चुके हैं। आख़िर यह कैसी मंत्रमुग्धता है कि हिन्दुओं में बड़े-बड़े अक़्लवाले विद्वान मौजूद हैं लेकिन कोई इस समस्या पर ग़ौर नहीं करता। यहाँ तक कि गाँधी जी जैसे सूझ-बूझ रखनेवाले और दुनिया देखे हुए लीडर भी मज़हबियत की उस नाव पर सवार हैं जिसे लोगों ने ऐसे ही कुछ मसलों पर जोड़ मिलाकर बना लिया है। आप इस गाय की पूजा पर रौशनी डालें और वाज़ेह करें कि यह कब से शुरू हुई और कैसे फैली। मुमकिन है कि कुछ हक़-पसन्द हिन्दू मुत्मइन हो जाएँ और अपनी क़ौम का सुधार करें।
(2) आवागमन का अक़ीदा (धारणा) हिन्दू क़ौम के यहाँ बुनियादी अहमियत रखता है। मैं नहीं कह सकता कि हिन्दुओं के अलावा कोई दूसरी क़ौम भी इसकी क़ायल हुई है या नहीं। फिर भी यह अक़ीदा भी संजीदा तनक़ीद (समीक्षा) चाहता है।
(3) सिख क़ौम की मज़हबी किताब, “गुरु ग्रंथ साहिब" सिर्फ़ अख़्लाक़ी नसीहतों और उपदेशों का संग्रह है। इसको विषयों और बहसों के लिहाज़ से गुलिस्ताँ, बोस्ताँ जैसी किताबों की सफ़ में रखा जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि अलग-अलग मज़हबों के नेक, अच्छे और सूफ़ियाना सोच रखनेवाले बुज़ुर्गों के फ़रमानों और उपदेशों को इसमें जमा कर दिया गया है। किताब की तरतीब करनेवाले का मंशा कुछ और मालूम होता है मगर उस मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ अब यह एक क़ौम की इलहामी (अवतरित) किताब बन गई है। जबकि इसमें न तो तमद्दुनी (सांस्कृतिक) मसलों से बहस है और न समाज से कोई सरोकार, न ही आर्थिकता और राजनीति में इससे कोई मदद व रहनुमाई मिल सकती है, मगर मेरी अक़्ल काम नहीं करती कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे और विद्वान लोग भी किस तरह इसपर मुतमइन हैं।
जवाब
आपने जिन बातों के बारे में सवाल किया है उनमें से हर एक तफ़सीली जवाब चाहता है। लेकिन मेरे लिए इस वक़्त इन चीज़ों पर तफ़सीली बहस करना मुश्किल है। नम्बरवार तीनों मसलों पर संक्षेप में अपने विचार रखता हूँ।
(1) हिन्दू मज़हब के बारे में मेरी मालूमात इतनी ज़्यादा वसीअ (व्यापक) नहीं हैं कि मैं उसके किसी मसले पर तहक़ीक़ी बहस कर सकूँ और बिना पूरी जानकारी के किसी चीज़ पर बहस व अलोचना करना मुनासिब नहीं है। जो भी थोड़ी-बहुत जानकारी मुझे हासिल है उसकी बुनियाद पर मैं इतना कह सकता हूँ कि पुराने ज़माने में, जिसको वैदिक दौर कहा जाता है, गाय के मुक़द्दस होने और पाकी का यह अक़ीदा मौजूद न था, या अगर था भी तो बिल्कुल शुरुआती हालत में था। चुनांचे इस बात के सुबूत मौजूद हैं कि उस दौर में हिन्दू गाय की क़ुरबानी किया करते थे। क़ौमों के इतिहास से भी यह साबित है कि प्राचीन आर्यजाति बंजारों की सभ्यता से ताल्लुक़ रखती थी जिसमें गाय की पूजा बिल्कुल नहीं थी। बाद में इसका साबक़ा उस मादरी तहज़ीब से हुआ जो भारत वर्ष की द्राविड़ी क़ौमों और इराक़, पश्चिमी एशिया और मिस्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता की क़ौमों का पेशा खेती-बाड़ी था और इनमें गाय के मुक़द्दस (पवित्र) होने की बात पाई जाती थी। इसलिए तहक़ीक़ इसी तरफ़ हमारी रहनुमाई करती है कि जिस तरह बनी-इस्राईल को मिस्र से गाय को मुक़द्दस मानने की छूत लगी, उसी तरह प्राचीन आर्यों को भी यह छूत भारत में आकर लगी है। जहाँ तक गाय की पूजा का ताल्लुक़ है वह तो हिन्दुओं के एक ख़ास तबक़े में ही पाई जाती है। लेकिन इसकी पवित्रता पूरी क़ौम में फैली हुई है। बल्कि जो लोग हिन्दुओं से निकलकर इस्लाम या ईसाई मज़हब में दाख़िल हुए हैं, उनके भी एक अच्छे-ख़ासे लोगों में इसका कुछ न कुछ असर सिर्फ़ इसलिए पाया जाता है कि उनका ज़ेहन पूरी तरह बदल नहीं सका है।
ख़ास तौर पर इस अक़ीदे को रद्द करने के लिए कुछ कहना शायद फ़ायदेमंद न होगा। क्योंकि एक ग़लत अक़ीदा बहुत-से दूसरे ग़लत अक़ीदों के साथ जुड़ा होता है, और एक उन सबकी अस्ल जड़ हुआ करती है। जब तक जड़ और शाख़ों के पूरे सिलसिले का सुधार न किया जाए सिर्फ़ किसी एक शाख़ को ठीक करने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। इस क़िस्म के तमाम ग़लत अक़ीदों की जड़ यह है कि इनसान इस कायनात के निज़ाम और इसमें अपने सही मक़ाम और कायनात के मालिक के साथ अपने और दूसरी चीज़ों के ताल्लुक़ की हालत को समझने में ग़लती करता है। इस शुरुआती और बुनियादी ग़लतफ़हमी से नतीजे के तौर पर बेशुमार ग़लतफ़हमियों का सिलसिला पैदा हो जाता है; वे सब एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक पूरी वैचारिक-व्यवस्था और जीवन-व्यवस्था पैदा कर देती हैं। अगर कोई शख़्स इस बात को समझ ले कि इस सारी कायनात का एक ही पैदा करनेवाला और एक ही मालिक, स्वामी और एक ही हाकिम व मुदब्बिर (प्रबन्धक) है और इनसान दुनिया में उसके ख़लीफ़ा व नायब की हैसियत से पैदा किया गया है और दुनिया की सारी चीज़ें इनसान के लिए ख़ादिम (सेवक) बनाई गई हैं तो ऐसा शख़्स शिर्क और ख़ुदा की पैदा की हुई चीज़ों की परस्तिश और माद्दी या रूहानी या ख़याली चीज़ों के मुक़द्दस होने के हर शक-सन्देह से ख़ुद-बख़ुद पाक हो जाएगा। उसके दिल में एक ख़ुदा के सिवा किसी की बन्दगी और किसी की पवित्रता के लिए जगह बाक़ी नहीं रहेगी। फिर अगर किसी शख़्स में सही क़िस्म का माक़ूल पसन्दाना व्यवहा (True Rationalism) मौजूद हो तो वह पुरखों के दौर से चले आ रहे तास्सुबात (भेद-भाव) और शख़्सी और नफ़्सानी तास्सुबात से ख़ुद-ब-ख़ुद ख़ाली हो जाएगा और अपनी सोच और अपने अमल को पूरी बेलौसी (निस्स्वार्थ भाव) के साथ इस तरीक़े पर क़ायम करेगा जो सरासर माक़ूल हो।
आपको इस बात पर ताज्जुब है कि हिन्दुओं में बड़े-बड़े आदमी मौजूद हैं जो गहरा इल्म और वसीअ नज़र रखते हैं मगर फिर भी इन अक़ीदों और ख़यालों में मुबतला हैं जो सरसरी नज़र में भी जाहिलियत के अक़ीदे और विचार महसूस होते हैं। इस प्रकार की हैरत आप ने आख़िरी सवाल के सिलसिले में भी ज़ाहिर की है। लेकिन आप देखेंगे कि यह सूरते-हाल महज़ किसी एक क़ौम ही के साथ मख़सूस नहीं है बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। दुनिया में बहुत-से ग़लत सोच और ग़लत अक़ीदे पर क़ायम निज़ाम पाए जाते हैं और उनमें से हर एक के माननेवालों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे और बहुत बुद्धिमान और समझदार और अपने मसलक (दस्तूर) की ख़ास गुमराहियों के सिवा दुनिया के तमाम दूसरे मामलों में इंतिहाई दर्जे के अक़्लमंद होंगे। इसके बावुजूद उन लोगों का ऐसी-ऐसी गुमराहियों में फँसे होना जिनमें से कुछ तो उनके ख़ास मसलक को माननेवालों के सिवा दूसरे तमाम लोगों को साफ़ तौर पर अक़्ल के ख़िलाफ़ महसूस होती हैं, देखने में एक हैरान करनेवाला मामला नज़र आता है। मगर इसकी हक़ीक़त पर ग़ौर किया जाए तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं रहती। इस सूरते-हाल की पहली वजह तो यह है कि इनसानों में ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो अपनी अक़्ल और इल्म के इस्तेमाल को ज़्यादातर अपने दुनियावी कारोबार और अपने शारीरिक जीवन के मामलों और मसलों तक सीमित रखते हैं और इसकी कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करते कि जिन फ़िक्री और अख़्लाक़ी बुनियादों पर उन्होंने अपनी ज़िन्दगी को बना रखा है या जिन बुनियादों पर बना बनाया जीवन उन्होंने पहले से पाया हुआ है उनके बारे में ख़ूब खोजबीन कर लें कि वे अपने आपमें सही भी हैं या नहीं। और उनसे बेहतर बुनियादें कहीं उनको मिल सकती है या नहीं। इसकी दूसरी वजह यह है कि इनसानों में बहुत ही कम आदमी ऐसे हैं जो नसली, क़ौमी, शख़्सी, नफ़सानी तास्सुबात से आज़ाद होकर ख़ालिस इल्मी तहक़ीक़ और ख़ालिस माक़ूलियत (बुद्धिमत्ता) पर अपने विचार और अमल के ढंग की बुनियाद रखने के लिए आमादा हों। हालांकि इसका दावा करनेवाले आपको बहुत मिलेंगे।
(2) आवागमन का अक़ीदा हिन्दुओं के अलावा कुछ दूसरी क़ौमों में भी पाया गया है और अब भी पाया जाता है और हिन्दुस्तान से बाहर भी कुछ फ़लसफ़ियाना निज़ामों (दार्शनिक-व्यवस्थाओं) में इसका निशान मिलता है। लेकिन हिन्दुस्तान में जितनी ज़्यादा गहरी जड़ें इसने पकड़ी हैं इसकी मिसाल दूसरी जगह नहीं मिलती। इस अक़ीदे की जड़ दो सवाल हैं जिनको इनसान ने हमेशा हल करने की कोशिश की है और अकसर अपने आपको मुख़्तलिफ़ शक्लों में आदमी के सामने लाते रहते हैं। पहला सवाल यह है कि दुनिया में मुसीबतें और आफ़तें (जिन में मौत भी शामिल है) क्यों पाई जाती हैं? पूरी राहत, ख़ुशी, लज़्ज़त, सलामती व आराम और हमेशा की ज़िन्दगी ही क्यों नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि इनसानी दिमाग़ के तबई (प्राकृतिक) नतीजे तो इस दुनिया में एक मुक़र्रर ज़ाबिते (विधान) के तहत निकलते नज़र आते हैं, लेकिन अख़लाक़ी नतीजे (जिनके ज़ाहिर होने की इनसानी फ़ितरत आप-से-आप माँग करती है) क्यों एक मुक़र्रर ज़ाबिते के मुताबिक़ ज़ाहिर नहीं होते? अगर वे सब या उनका एक हिस्सा ज़ाहिर होने के लिए रुका हुआ है तो उसके ज़ाहिर होने की शक्ल क्या है?
इन दोनों सवालों के बहुत-से अलग-अलग जवाब बहुत-से फ़लसफ़ियाना निज़ामों में मिलते हैं। मगर इन सबपर इस छोटी बहस में बात-चीत नहीं की जा सकती।
हिन्दुस्तान के फ़लसफ़े ने, जिनकी कल्पनाओं ने आगे चलकर मज़हब की शक्ल ले ली, इन सवालों को कर्म और 'आवागमन' के अक़ीदे की शक्ल में हल किया है। वे इस दुनिया को परीक्षास्थल के बजाय एक अज़ाब का घर और एक तरह के जेलख़ाने की हैसियत से देखते हैं। जिस्मानी ज़िन्दगी को अस्ल में मुसीबत समझते हैं और जिस्म और जिस्मानियत के साथ उनके ताल्लुक़ को इस बात की वजह क़रार देते हैं कि रूह (आत्मा) जिस्म की क़ैद से छूट-छूटकर बार-बार फिर उसी क़ैदख़ाने में वापस आती है। उनके नज़दीक मुसीबतें, आफ़तें और दुख-तकलीफ़ और इसी तरह ख़ुशहालियाँ और कामयाब ज़िन्दगियाँ, उन बुरे या अच्छे अमलों (कर्मों) का नतीजा हैं जो रूह ने उस वक़्त किए थे जब वह मौजूदा ज़िन्दगी के पहले जिस्म रूपी क़ैदख़ाने में थी। इसके अलावा भी उनका ख़याल यह है कि आमाल (कर्मों) के जो अख़लाक़ी नतीजे एक ज़िन्दगी में पूरी तरह या अपनी अस्ल शक्ल में ज़ाहिर नहीं होते, उनके ज़ाहिर होने की सूरत इसके सिवा कुछ नहीं है कि इनसान इसी दुनिया में बार-बार आकर उनको वुसूल करता रहे।
यह एक वसीअ फ़िक्री निज़ाम है जिसका सिर्फ़ एक ख़ुलासा मैंने बयान किया है। यह पूरी ज़िन्दगी के बारे में इनसान के नुक़्त-ए-नज़र (दृष्टिकोण) और ज़िन्दगी के हर पहलू के मुताल्लिक़ उसके रवैये पर असर डालता है। उसके तमाम फ़िक्री व अमली नतीजों पर यहाँ बहस करना मुश्किल है। मैं सिर्फ़ इतना कह देना काफ़ी समझता हूँ कि अस्ल में यह क़यासी फ़लसफ़ों (Speculative Philosophies) की ही तरह की चीज़ है और इस तरह की तमाम फ़लसफ़ियाना (दार्शनिक) निज़ाम की बुनियादी ख़ासियत यह है कि उनके सामने जो मसले आते हैं उनको वे सिर्फ़ ख़याल, सोच, मन्तिक़ (तर्क) और अटकल से किसी ऐसे तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको अपनी हद तक अपने सामने आए हुए मसलों का इत्मीनानबख़्श और दिल को लगता हुआ जवाब मिल जाए। इस बात की परवाह किए बग़ैर कि इल्म, तजरबा, मुशाहिदा (अवलोकन) और कायनात की निशानियों से उसकी कोई शहादत (गवाही) मिले या न मिले, क़यासी फ़लसफ़ी इस शहादत (गवाही) की सिरे से कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं करती। उसे तो केवल अपने पेशे-नज़र सवालों का ऐसा जवाब दरकार होता है जिस पर वह और उस जैसी सोच रखनेवाले लोग मुत्मइन हो जाएँ। मगर यह ज़ाहिर है कि ऐसे क़यासों (अनुमानों) का सही बात और किसी बात का रूह की हक़ीक़त के मुताबिक़ होना कुछ ज़रूरी नहीं है बल्कि इसकी बहुत कम उम्मीद की जा सकती है। यह तो एक तीर है जो अंधेरे में अटकल से चलाया जाता है, निशाने पर लगे या न लगे। तीर चलानेवाले को ख़ुद भी इसकी कोई परवाह नहीं होती। बल्कि वह इसकी भी परवाह नहीं करता कि किसी जगह उसके लगने से 'खट' की आवाज़ भी आती है या नहीं। उसको मुत्मइन करने के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि अपने अनुमान से उसने जिसको निशाने का सही रुख़ समझा उस तरफ़ अपनी हद तक ठीक-ठीक सीध बाँधकर तीर चला दिया। ऐसी तीरन्दाज़ी के निशाने पर लगने की जितनी कुछ उम्मीद की जा सकती है उतनी ही कुछ क़यासी फ़लसफ़ों के मुताबिक़ हक़ीक़त होने की भी उम्मीद की जा सकती है।
आवागमन के बहुत-से माननेवाले ख़ुद भी अपने अक़ीदे की इस ख़ामी को महसूस करते हैं। यह उसी ख़ामी को पूरा करने की कोशिश है जो कभी-कभी अख़बारों में किसी ऐसे बच्चे या बच्ची के ज़ाहिर होने की ख़बर की शक्ल में आती रहती है जो अपने पिछले जन्म की बातों को बताता या बताती है। लेकिन अव्वल तो यही अजीब बात है कि ऐसे बच्चे सिर्फ़ हिन्दुओं ही में पैदा होते हैं और हिन्दू अख़बारों तक ही उनकी ख़बर पहुँचती है।
दूसरी इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये लोग अपने फ़लसफ़े की ताईद (समर्थन) में मुशाहिदे व तजरबे (आँखों देखी गवाही) के न होने की तलाफ़ी के लिए कहीं एक-आध ऐसे बच्चे की पैदाइश को काफ़ी समझ लेते हैं। हालाँकि उनके नज़रिए के सही होने के लिए यह ज़रूरी है कि सारे ही बच्चे ऐसे पैदा हों। अगर वह सज़ा या जज़ा (इनाम) जो इनसान को एक जन्म के आमाल (कर्मों) की बुनियाद पर दूसरे जन्म में मिलती है क़ुदरती जज़ा या सज़ा नहीं बल्कि अख़लाक़ी जज़ा व सज़ा है, तो हर इनसान को इसका शऊर हासिल होना चाहिए कि वह किस चीज़ की जज़ा या सज़ा पा रहा है। क्योंकि तमाम अख़लाक़ी आमाल लाज़िमी तौर पर जाने-पहचाने अमल होते हैं और उनका नतीजा भी लाज़मी तौर पर जाना-पहचाना होना चाहिए।
इस तरीक़े के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने अक़्ल और उसकी माँगों और फ़ितरत और उसके तक़ाज़ों और कायनात की निशानियों और उसके इशारों को नज़र-अन्दाज़ करके ठेठ ज़ाहिर बीनी के साथ, और एक बड़ी हद तक मज़हबी ढंग और फ़िक्र से इनकार की ख़ाहिश के साथ तजरबे व मुशाहिदे पर अपनी राय की बुनियाद रखी है, उन्होंने पहले सवाल की जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, बल्कि अपनी तहक़ीक़ और राय को "क्यों है" के सवाल के बजाय बड़ी हद तक सिर्फ़ “क्या है" के सवाल तक महदूद रखा। रहा दूसरा सवाल तो उसके बारे में उन्होंने किसी न किसी तरह अपने मन को इस जवाब ही पर मुत्मइन करने की कोशिश की कि सारे अख़लाक़ी नतीजे बस इसी दुनिया की एक ही ज़िन्दगी में ज़ाहिर हो लेते हैं जो मौत पर ख़त्म हो जाती है, और अगर मान लीजिए कि वे ज़ाहिर नहीं होते तब भी किसी हाल में मौत के बाद कोई ज़िन्दगी नहीं है, क्योंकि वह न हमारे तजरबे में आई और न ही हमने उसको अपनी आँखों से देखा। लेकिन इनसान चाहे जितनी भी कोशिश करे इस जवाब से उसके दिल का इत्मीनान किसी तरह मुमकिन नहीं।
अब रही यह बात कि नबियों के लाए हुए दीन में इन दोनों सवालों का क्या जवाब है और वे किन दलीलों से बिलकुल अक़्ल के मुताबिक़ जवाब है, तो इसपर मैं अपनी किताबों जैसे 'रिसाला दीनियात', 'इस्लामी तहज़ीब और उसके उसूल व मबादी', 'ज़िन्दगी बाद-मौत', 'इस्लाम और जाहिलियत', और क़ुरआन की सूरा आराफ़ की तफ़सीर में तफ़सील के साथ बयान कर चुका हूँ, लिहाज़ा यहाँ उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यह बात साफ़ कर देना मैं जरूरी समझता हूँ कि फ़ितरत से परे मामलों में यह उसूल है कि उनका कोई हल भी, चाहे वह नकारात्मक रूप में हो या सकारात्मक रूप में, ऐसा पक्का सुबूत कभी नहीं हो सकता जैसे दो और दो का चार होना एक दम पक्का सुबूत है कि इसको मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसे मसलों का ज़्यादा से ज़्यादा माक़ूल हल जिसके मुताबिक़ हक़ीक़त होने का ग़ालिब गुमान किया जा सकता हो, सिर्फ़ वही हो सकता है जो अक़्ल और फ़ितरत के तमाम माँगों और तक़ाज़ों को पूरा कर सकता हो। जिसकी तरफ़ कायनात की निशानियों, और तजरबों और मुशाहिदों (अवलोकनों) में साफ़-साफ़ इशारे पाए जाते हों। जिससे ज़िन्दगी के उन तमाम मसलों को हल किया जा सकता हो जो इस ख़ास मसले से दूर या क़रीब का ताल्लुक़ रखते हैं जिस पर अक़्ल के मुताबिक़ किसी एतिराज़ की गुंजाइश न हो। जिसके मान लेने से कुछ दूसरे ऐसे मसले न पैदा होते हों जिनका हल मुमकिन न हो जिसके मानने से कुछ ऐसी मुश्किलें न पैदा होती हों जिन्हें किसी दूसरे तरीक़े से दूर करना मुमकिन न हो और जिसके ख़िलाफ़ कोई सुबूत न दिया जा सकता हो। अक़्ल ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालों के किसी हल को ख़ास मसले (Most Probable) के तौर पर समझने की हद तक ही हमें ले जा सकती है। इसके आगे यक़ीन हासिल करने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि ऐसा हल पेश करनेवालों की ज़िन्दगियों को उनके पेश किए हुए पूरे निज़ामे-फ़िक्र व अमल की माक़ूलियत को और उनके काम और उसके नतीजों को देखकर उनपर बिन देखे ईमान लाया जाए।
(3) गुरु ग्रन्थ साहिब का मुताला मैंने ख़ुद तो नहीं किया है लेकिन जिस हद तक मैंने मुताला करनेवालों से मालूमात हासिल की हैं उनकी बुनियाद पर मैं आपके इस ख़याल से सहमत हूँ कि सिख मज़हब सिर्फ़ एक सूफ़ियाना मज़हब है और इसमें इनसान की ज़िन्दगी के बड़े-बड़े मसलों जैसे कि तमद्दुन, मआशरत (संस्कृति व समाज) राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, अदालत व क़ानून, जंग और सुलह आदि के बारे में कोई ऐसी हिदायत मौजूद नहीं है जिसपर दुनिया में एक समाज और एक स्टेट (राज्य) का निर्माण हो सके। लेकिन जिस वजह से सिखों के ख़ासे पढ़े-लिखे और सूझ-बूझ रखनेवाले लोग अपने हक़ की खोज और हिदायत की तलाश को छोड़कर इस मज़हब पर राज़ी और मुतमइन हैं इसका तफ़सीली बयान मैं पहले सवाल के जवाब में कर चुका हूँ।(तर्जमानुल-क़ुरआन, जनवरी 1946 ई.)
----------------------------
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
Subscribe Our You Tube Channel
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
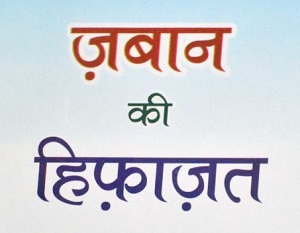
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
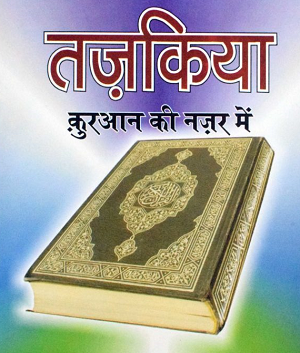
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

