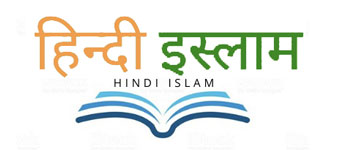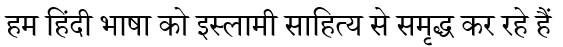फ़िक़्हे-इस्लामी : इस्लामी ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग (फ़िक़्हे-इस्लामी : लेक्चर- 1)
-
फ़िक़्ह
- at 25 December 2024
दो शब्द
मुहाज़रात (लेक्चर्स) के सिलसिले की यह तीसरी कड़ी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए दिलो-दिमाग़ अल्लाह तआला के सामने शुक्र और इत्मीनान की भावनाओं से भरे हुए हैं। इस सिलसिले के पहले दो भाग मुहाज़राते-क़ुरआन और मुहाज़राते-हदीस के शीर्षक से इससे पहले प्रस्तुत किए जा चुके हैं। देश के विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने इस तुच्छ लेखक को जिस प्रकार प्रोत्साहित किया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ।
यह किताब फ़िक़्हे-इस्लामी के एक सामान्य परिचय पर आधारित है, जिसमें फ़िक़्हे-इस्लामी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बारह शीर्षकों के तहत समोने की कोशिश की गई है। फ़िक़्हे-इस्लामी एक अथाह समुद्र है, जिसकी विशालताओं को किसी एक भाग तो क्या दर्जनों भागों में समेटना भी मुश्किल है। अलबत्ता यह कोशिश की गई है कि फ़िक़्हे-इस्लामी के महत्वपूर्ण विषयों, मूल चर्चाओं, मूल धारणाओं और ज़रूरी पहलुओं को सरल एवं सरस भाषा में आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों की सेवा में पेश किया जाए।
उर्दू/हिन्दी जाननेवाले पाठकों में फ़िक़्हे-इस्लामी से दिलचस्पी रखने और इस ओर ध्यान देनेवाले लोगों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका सम्बन्ध क़ानून और वकालत के विभाग से है। जिनको अपने नित्य के कामों के करने के दौरान बहुत-से मामलों के बारे में फ़िक़्हे-इस्लामी की राय जानने की आवश्यकता पड़ती है। फ़िक़्हे-इस्लामी पर जो किताबें उर्दू या अंग्रेज़ी भाषा में आम तौर पर उपलब्ध हैं वे यह काम नहीं कर पातीं। उर्दू भाषा में उपलब्ध किताबों की बड़ी संख्या अरबी से अनुवाद की हुई है। अनुवादों की कमज़ोरी से परे ये किताबे एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त क़ानून विशेषज्ञ के सवालों का जवाब उसके जाने-माने ढंग और मुहावरे में नहीं देतीं। अरबी की प्राचीन पुस्तकें, जिनके ज्ञान सम्बन्धी महत्व का किसी हद तक अंदाज़ा इस किताब के अध्ययन से हो सकेगा, ऐसे लोगों के लिए नाकाफ़ी, बल्कि कभी-कभी अलाभकारी साबित होती हैं जो इस्लामी ज्ञान में विशेष योग्यता न रखते हों और फ़िक़्हे-इस्लामी की मूल धारणाओं से पूरी तरह परिचित न हों। इसके अलावा अरबी की प्राचीन फ़िक़्ह की पुस्तकों के सम्बोधित व्यक्ति वे फुक़हा (धर्मशास्त्री) थे जो अपने-अपने ज़माने में इज्तिहाद करने और फ़तवा देने के पद पर रह चुके थे। वे इस्लामी उलूम की विशेष योग्यता, फ़िक़्हे-इस्लामी की मूल धारणाओं और मूल चर्चाओं से भली-भाँति परिचित और इस अथाह समुद्र के पुराने तैराक थे। उनको फ़िक़्हे-इस्लामी के मौलिक सिद्धान्तों की नहीं आम तौर से गौण एवं आंशिक बातों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए ये किताबें प्राय: उन्हीं की आवश्यकता को सामने रखकर लिखी गईं। यही वजह है कि फ़िक़्हे-इस्लामी की अधिकतर किताबों का ज़ोर फ़िक़्ही जुज़इयात (छोटी-छोटी बातों) पर ही रहता है, मूल सिद्धान्तों से बहस करने की उनमें न गुंजाइश होती है न आवश्यकता। इसके अलावा किसी भी ज्ञान एवं कला की तरह फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह के मूल सिद्धान्तों को बयान करने का अंदाज़ और शैली भी हर ज़माने में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ एक ज़माना फ़िक़्ह के चार बड़े इमामों का ज़माना था, जब इन मूल सिद्धान्तों को विशुद्ध धार्मिक अवधारणाओं और शिक्षाओं की भाषा और शैली में बयान किया जाता था। चुनाँचे इमाम शाफ़िई और इमाम मुहम्मद-बिन-शैबाई और उन जैसे दूसरे फुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) के लेखों में शरीअत के मूल सिद्धान्तों से बहस करने का एक ख़ास अंदाज़ पाया जाता था। फिर जल्द ही एक दौर ऐसा आया जब फ़िक़ही और उसूली बहसों को मंतिक़ (तर्कशास्त्र) और फ़लसफ़ा (दर्शन) की शैली में बयान किया जाने लगा। इस शैली का उच्च श्रेणी का नमूना इमाम ग़ज़ाली और इमाम राज़ी की किताबों में नज़र आता है। यह शैली मुतक़द्दिमीन (प्राचीन विद्वानों) की शैली से बिलकुल भिन्न है। आधुनिक समय में पश्चिम की धारणाओं और चर्चाओं ने फ़िक़्हे-इस्लामी की बहसों और चर्चाओं की शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। आज अरब दुनिया में फ़िक़्हे-इस्लामी पर जो किताबें लिखी जा रही हैं उनमें अधिकांश पश्चिमी क़ानूनों की शैली और धारणाओं के अनुसार लिखी जा रही हैं। इन हालात में आवश्यकता इस बात की है कि उर्दू (और हिन्दी) भाषा में भी इस नई शैली के अनुसार किताबें तैयार की जाएँ, ताकि क़ानूनविद् और वकालत पेशा लोग ज़्यादा बेहतर और प्रभावकारी ढंग से फ़िक़्हे-इस्लामी के पक्ष को समझ सकें।
फ़िक़्हे-इस्लामी से दिलचस्पी रखनेवाले लोगों में दूसरे नम्बर पर वे उलमा (इस्लामी विद्वान) आते हैं जो फ़िक़्ह या इफ़्ता (फ़तवा देने) की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। यों तो उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति का सामान प्राचीन किताबों और इस सम्बन्ध में लिखी गई बड़ी किताबों से हो जाता है, लेकिन एक हद तक इन लोगों को भी इसकी आवश्यकता है कि उनके लिए फ़िक़्हे-इस्लामी के विषयों को नए ढंग से पेश किया जाए। इन विद्वानों के लिए यह उचित होगा कि वे फ़िक़्हे-इस्लामी पर लिखे जानेवाले इस समय के लेखों से न केवल परिचित हों, बल्कि नई शैली को अपनाने में भी किसी झिझक एवं संकोच का प्रदर्शन न करें। यों उनको फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष बयान करने में भी सहायता मिलेगी, और फ़िक़्हे-इस्लामी के इस नए दौर को जानने-समझने में भी आसानी होगी।
फ़िक़्हे-इस्लामी से दिलचस्पी रखनेवालों में तीसरे नम्बर पर यूनिवर्सिटियों और आधुनिक शिक्षण संस्थानों से जुड़े वे लोग हैं जिन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी का सामान्य रूप से एक सरसरी-सा अध्ययन किया है और ज़्यादा विस्तृत ढंग से फ़िक़्हे-इस्लामी के पक्ष को जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए उर्दू भाषा में ऐसी किताबों की तैयारी बहुत ज़रूरी है जिसमें उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि और शैली तथा मुहावरों के अनुसार फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष अत्यन्त प्रमाणित स्रोतों की सहायता से बयान किया गया हो। आज फ़िक़्हे-इस्लामी के बारे में जो ग़लत-फ़हमियाँ पाई जाती हैं उनका एक बड़ा कारण ऐसे लिट्रेचर का अभाव भी है जिससे ये तीनों प्रकार के लोग लाभान्वित हो सकें और एक प्रभावकारी ढंग से फ़िक़्ह का पक्ष बयान कर सकें। यह किताब इस मक़सद को पूरा करने की एक मामूली-सी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि यह किताब न केवल फ़िक़्हे-इस्लामी के छात्रों, वकीलों और क़ानूनविद् लोगों के लिए उपयोगी और दिलचस्प साबित होगी, बल्कि आम शिक्षित लोग भी इसके ज़रिये बहुत-से मामलों में फ़िक़्हे-इस्लामी के पक्ष को उसकी सही पृष्ठभूमि में समझ सकेंगे और आधुनिक समय में इसकी सार्थकता का अनुमान कर सकेंगे।
ये लेक्चर्स सितंबर-अक्तूबर 2004 में रिकार्ड और फिर कम्प्यूटर पर कम्पोज़ किये गए। फ़िक़्ह के बाद अब अगर अल्लाह ने मौक़ा दिया तो सीरत और उसके बाद फ़िक्रो-अक़ीदा पर लेक्चर का भी प्रोग्राम है। देखिए उसके साधन कब उपलब्ध होते हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि इस तुच्छ प्रयास को अपने यहाँ स्वीकार कर ले, इसको छात्रों और पाठकों के लिए लाभकारी बनाएँ।
डॉक्टर महमूद अहमद ग़ाज़ी
13 जून 2005 ई॰
इन लेक्चर्स का उद्देश्य
इन लेक्चर्स का उद्देश्य फ़िक़्हे-इस्लामी के विषयों और उनमें बयान सारा विवरण प्रस्तुत कर देना नहीं है। इसलिए कि बारह लेक्चर तो क्या बारह वर्ष में भी कोई व्यक्ति फ़िक़्हे-इस्लामी की विशालताओं को बयान नहीं कर सकता। यह एक ऐसा अथाह समुद्र है जिसकी गहराइयों का अनुमान उन्हीं लोगों को हो सकता है जो इस नदी के तैराक हैं। इन लेक्चर्स का उद्देश्य केवल यह है कि उन लोगों को, जिन्होंने पवित्र क़ुरआन के अध्ययन को अपने जीवन का मूल लक्ष्य और क़ुरआन को दूसरों को समझाने को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु क़रार दिया है और जो पवित्र क़ुरआन के पढ़ने-पढ़ाने में व्यावहारिक रूप से लगे हैं, फ़िक़्हे-इस्लामी से इस तरह परिचित करा दिया जाए कि वे फ़िक़्हे-इस्लामी की व्यापकता, गहराई और मूल विशेषताओं से परिचित हो जाएँ। आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर का शीर्षक है ‘फ़िक़्हे-इस्लामी : इस्लामी ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग’। अगर इस्लामी ज्ञान-विज्ञान को एक गुलदस्ता से उपमा दी जाए तो इस गुलदस्ते का सबसे नुमायाँ फूल फ़िक़्हे-इस्लामी है।
फ़िक़्हे-इस्लामी के बारे में एक ग़लतफ़हमी
फ़िक़्हे-इस्लामी पर चर्चा करने से पहले एक ग़लत-फ़हमी अपने ज़ेहन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। यह ग़लत-फ़हमी कभी-कभी कम समझ या नादानी से, कभी-कभी किसी नकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप, कभी-कभी कम जानकार और कम-समझ लोगों से चर्चा के परिणामस्वरूप पैदा हो जाती है, और वह यह है कि फ़िक़्हे-इस्लामी पवित्र क़ुरआन और हदीसे-रसूल से अलग कोई चीज़ है। पवित्र क़ुरआन और फ़िक़्हे-इस्लामी, पवित्र क़ुरआन और हदीस और सुन्नत, यह एक ही हक़ीक़त के विभिन्न पहलू हैं और एक ही चीज़ को समझने के विभिन्न अंदाज़ हैं। अल्लाह की शरीअत हमारे पास पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रूप में आई है। अल्लाह की इस शरीअत को जब इंसान अपनी नित्य दिनचर्चा पर लागू करेगा तो उसको अपना पूरा जीवन, व्यक्तिगत और सामूहिक, हर दृष्टि से शरीअत के आदेशों के अनुसार ढालना होगा। इसके लिए पवित्र क़ुरआन के मार्गदर्शन और हदीसों की शिक्षाओं से आंशिक आदेश और ‘मसाइल’ (आदेशों का विवरण) मालूम करने पड़ेंगे। शरीअत के हर-हर आदेश पर ग़ौर करके गौण आदेशों को संकलित करना पड़ेगा। इसके लिए नित्य के मामलों पर शरीअत के आदेशों का लागू होना उसी समय सम्भव हो सकेगा जब इस काम का बेड़ा उठानेवाला गहरी समझ से काम लेगा। अब चाहे तो वह स्वयं इस गहरी समझ की क्षमता प्राप्त करके उससे काम ले, या दूसरी स्थिति में उन विद्वानों की गहरी समझ पर विश्वास करे जिनको दरकार ज्ञानपरक क्षमता प्राप्त हो। अत: हर वह व्यक्ति जो शरीअत के अनुसार जीवन गुज़ारना चाहता है वह यही नीति अपनाने पर मजबूर है। इसी अमल और तरीक़े-कार का नाम फ़िक़्ह है। पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल की नुसूस (स्पष्ट आदेशों) को नित्य घटित होनेवाली घटनाओं और तथ्यों पर चस्पाँ करना, और उनके विस्तृत आदेशों को संकलित करना, और संकलित करके उनके अनुसार जीवन को सँवारना, इस पूरी प्रक्रिया का नाम फ़िक़्ह है। यह प्रक्रिया एक पल और एक क्षण के लिए भी पवित्र क़ुरआन और सुन्न्त से अलग नहीं की जा सकती। पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा हैं। इस परम्परा के ज़ाहिरी परिणाम या व्यावहारिक निशानियों से सम्बन्धित मार्गदर्शन फ़िक़्ह के रूप में हमारे सामने आता है।
फ़िक़्हे-इस्लामी जिस रूप में आज हमारे पास मौजूद है, इस रूप में इसकी तैयारी और तर्तीब में मानव इतिहास के बेहतरीन दिमाग़ों ने हिस्सा लिया है। इस्लामी इतिहास में जो बेहतरीन दिमाग़ हुए हैं, उनका फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन, संगठन और विस्तारण में इतना असाधारण भाग है कि दुनिया की किसी और क़ौम के इतिहास में, या किसी और सभ्यता एवं संस्कृति में इसका उदाहरण नहीं मिलता। किसी दूसरी क़ौम के ज्ञानपरक एवं वैचारिक संग्रह में न इस गहराई का उदाहरण मिलता है, न इस विशालता का उदाहरण मिलता है और न इस तत्वदर्शितापूर्ण क्रम का उदाहरण मिलता है जो फ़िक़्हे-इस्लामी के संग्रह के रूप में हमारे सामने मौजूद है।
फ़िक़्हे-इस्लामी या इस्लामी क़ानून
कुछ लोग फ़िक़्ह का अनुवाद इस्लामी क़ानून या Islamic Law करते हैं। स्वयं समझने और छात्रों को समझाने के लिए हो सकता है यह अनुवाद सही हो। एक आम आवश्यकता के लिए इस अनुवाद को अपनाने में कोई हरज नहीं। लेकिन फ़िक़्हे-इस्लामी के विशेषज्ञों को यह याद रखना चाहिए कि फ़िक़्ह का अनुवाद इस्लामी क़ानून या इस्लामिक लॉ नहीं है। अंग्रेज़ी भाषा में जिस चीज़ को लॉ कहते हैं या उर्दू में ज्ञान के जिस विभाग के लिए क़ानून का शब्द प्रयुक्त होता है, वह फ़िक़्हे-इस्लामी के मुक़ाबले में बहुत सीमित, अत्यन्त निम्नस्तरीय और अत्यन्त हल्की चीज़ है। फ़िक़्हे-इस्लामी का दायरा, क़ानून और लॉ के मुक़ाबले में अत्यन्त विस्तृत, अत्यन्त व्यापक और अत्यन्त गहराई पर आधारित है। इसलिए अस्थायी रूप से अपनी समझ की ख़ातिर या एक कम जानकार को समझाने की ख़ातिर फ़िक़्हे-इस्लामी का अनुवाद इस्लामिक लॉ या इस्लामी क़ानून किया जा सकता है, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि यह अनुवाद अधूरा है।
फ़िक़्हे-इस्लामी और दुनिया के दूसरे क़ानून
फ़िक़्हे-इस्लामी पर बात करने से पहले यह बात मुनासिब मालूम होती है कि हम फ़िक़्हे-इस्लामी की एक बहुत आम और आरम्भिक तुलना दुनिया के दूसरे क़ानूनों के साथ करके यह देखें कि फ़िक़्हे-इस्लामी की वे कौन-कौन-सी नुमायाँ विशेषताएँ हैं जो इसको दूसरी प्राचीन और आधुनिक व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। अरबी के किसी कवि ने अपनी कविता के द्वारा यह बात कही है कि चीज़ें अत्यंत स्पष्ट और नुमायाँ होकर सामने आ जाती हैं अगर उनके विलोम से उनकी तुलना करके देखा जाए। रौशनी की हक़ीक़त समझ में आ सकती है अगर अंधेरे का ज्ञान हो। इल्म का मतलब मालूम हो सकता है अगर जहालत का पता हो। अक़्ल और समझ के महत्व का अनुमान हो सकता है अगर बेवक़ूफ़ी और मूर्खता से वास्ता पड़ चुका हो। इसलिए फ़िक़्हे-इस्लामी के महत्व का किसी हद तक अनुमान किया जा सकेगा। अगर एक सरसरी नज़र दुनिया के दूसरे क़ानूनों पर भी डाल ली जाए।
आज फ़िक़्हे-इस्लामी की गणना दुनिया की कुछ अति प्राचीनतम क़ानूनी व्यवस्थाओं में होती है। फ़िक़्हे-इस्लामी जिस दौर में संकलित हो रही थी, जिन दिनों इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) और अइम्मा मुज्तहिदीन (बड़े इमाम) और क़ुरआन के टीकाकार, क़ुरआन और सुन्नत पर ग़ौर करके क़ुरआन और सुन्नत के आदेशों को संकलित कर रहे थे। उस दौर में दुनिया में चार बड़े बड़े क़ानून मौजूद थे जिनकी गणना न केवल उस दौर के विकासवादी क़ानूनों में होती थी, बल्कि आज भी क़ानून के ज्ञान के इतिहास में इन क़ानूनों का अध्ययन दिलचस्पी और महत्व के साथ किया जाता है। प्राचीनतम क़ानून जो आज हमारे सामने है और जिसका टेक्स्ट दुनिया की हर बड़ी भाषा में प्रकाशित रूप में मौजूद है, वह हम्मूराबी का क़ानून है। हम्मूराबी हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) से लगभग पौने दो हज़ार वर्ष पहले गुज़रा है। उसकी मृत्यु का अनुमान 750 ईसा पूर्व किया जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का विचार है कि यह वही व्यक्ति है जिसको मुस्लिम जगत् नमरूद के नाम से जानता है। यह हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के समय में था। उसने क़ानूनों का एक संग्रह संकलित करवाया था जिसमें कई सौ धाराएँ हैं। यह शासक लगभग पैंतालीस वर्ष शासक रहा। उसने दुनिया का एक प्राचीनतम संग्रह जिसें कई सौ (कुल दो सौ बयासी धाराएँ) थीं, एक बड़ी पत्थर की तख़्ती पर खुदवाया था। आठ फ़ुट ऊँची यह तख़्ती जो उसके ज़माने में लिखी गई थी, 1901 ई॰ में उपलब्ध हुई। उसके बारे में पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह संकलित इतिहास में दुनिया का प्राचीनतम लिखित क़ानून का संग्रह है। अगर इस क़ानून का सरसरी जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अगर इंसान को अल्लाह तआला का और उसके भेजे हुए पैग़म्बरों (अलैहिस्सलाम) का मार्गदर्शन उपलब्ध न हो तो वह किस अंदाज़ का क़ानून संकलित करता है। यह बात कि इसका संकलित करनेवाला बुतपरस्त और मुशरिक था, इस क़ानून के आरम्भ से भी ज़ाहिर होता है और अन्त से भी स्पष्ट होता है।
हम्मूराबी का क़ानून और उसमें लिखा विवरण
हम्मूराबी के क़ानून का आरम्भ भी देवताओं के नाम अपीलों और प्रार्थनाओं से होता है और अन्त भी बुतों और देवताओं के सामने प्रार्थना के शब्दों पर होता है। जगह-जगह इस क़ानून में क़ानून के विरोधियों पर फिटकार की गई है। जो आदेश दिए गए हैं उनके न्याय पर आधारित और उचित होने का अनुमान आप इससे कर सकते हैं कि इस क़ानून के अनुसार झूठे गवाह की सज़ा मौत है। ग़लत फ़ैसला करनेवाले जज को जुर्माना भी किया जाए और नौकरी से निकाल भी दिया जाए। एक ज़्यादा दिलचस्प उदाहरण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी मकान, दुकान या किसी भी इमारत की दीवार गिर जाए, और उसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति मर जाए तो जिसने यह दीवार बनाई थी उसको सज़ा-ए-मौत दी जाएगी। अगर दीवार गिर जाने से मकान के मालिक का बच्चा मर जाए तो बनानेवाले मिस्त्री के बच्चे को मुजरिम क़रार देते हुए उसको सज़ा-ए-मौत दी जाए। उदाहरणार्थ एक ठेकदार ने मकान बनाया। उस मकान की दीवार गिर गई और जो आदमी उसमें रहता था उसका बच्चा दीवार तले आकर मर गया। तो अब सज़ा यह नहीं है कि बनानेवाले मिस्त्री या ठेकदार से पूछा जाए कि उसने यह कमज़ोर दीवार क्यों बनाई थी, बल्कि सज़ा यह है कि मिस्त्री के बच्चे को पकड़कर क़त्ल कर दिया जाए। यह दुनिया के प्राचीनतम क़ानून की एक धारा है।
इस क़ानून के तहत इंसानी आबादी एक तरह के इंसानों पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसने आबादी को तीन वर्गों में बाँट रखा था। एक वर्ग अधिकारियों या कुलीन वर्ग का, एक जन साधारण का और एक ग़ुलामों का वर्ग। लेकिन इन आदेशों के बावजूद हम यह देखते हैं कि इस क़ानून में कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे अनुमान होता है कि जब यह क़ानून संकलित किया जा रहा था तो वहाँ कुछ आसमानी शरीअतों के अवशेष भी मौजूद थे। इन आसमानी शरीअतों के अवशेष बज़ाहिर हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम), हज़रत इदरीस (अलैहिस्सलाम) या किसी और प्राचीनतम पैग़ंबर की शरीअत के थे जिनको हम नहीं जानते। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ आसमानी किताबें या कम-से-कम उनकी बची हुई शिक्षाएँ वहाँ मौजूद थीं, जिनके प्रभाव इस क़ानून में पाए जाते हैं। तलाक़ के कुछ आदेश और सज़ाओं के कुछ आदेश, तौरात और पवित्र क़ुरआन के आदेशों से मिलते-जुलते मालूम होते हैं। उदाहरण के रूप में आँख के बदले आँख और कान के बदले कान का सिद्धान्त अपनाया गया है। चोर के लिए हाथ काटने की सज़ा का क़ानून भी हम्मूराबी के यहाँ मिलता है। इस क़ानून में लाँछन लगाने के लिए कठोर दंड प्रस्तावित किया गया है। व्यभिचार को फ़ौजदारी अपराध क़रार देते हुए उसके लिए मृत्युदंड रखा गया है। घरेलू मामलों में भी कुछ आदेश आसमानी शरीअतों से प्रभावित मालूम होते हैं। उदाहरण के रूप में तलाक़ का अधिकार पुरुष को प्राप्त है।
रोम का क़ानून
हम्मूराबी क़ानून के अलावा दुनिया का दूसरा प्राचीन क़ानून यहूदी क़ानून है। फिर शायद हिंदुओं का मनुशास्त्र (मनुस्मृति) है। फिर पश्चिम जगत् का वह क़ानून जिसपर पश्चिमवालों को आज भी गर्व है, रोमन लॉ है। यह वह क़ानून है जिसका आरम्भ भी ईसा पूर्व चौथी या पाँचवीं सदी से होता है। यह क़ानून पहली बार 450 ईसा पूर्व में बारह तख़्तियों पर संकलित ढंग से लिखा गया। क़ानून का अधिकांश भाग पिछली से प्रचलित रस्मों-रिवाजों से भरा था। कुछ आदेश दूसरी क़ौमों, उदाहरणार्थ यूनानियों, से लिए गए बताए जाते हैं। इन बारह तख़्तियों पर लिखे आदेशों में कुछ क़ानूनी ज़ाब्तों के अलावा धार्मिक रस्मों और जनाज़े और मय्यत के आदेश भी शामिल थे। शैली में क़ानूनी तक़ाज़ों और दोटूक अंदाज़ के बजाय शायराना और अतिशयोक्तिपूर्ण शैली अपनाई गई है। क़ानूनी आदेश बहुत सख़्त और कुछ जगह अव्यावहारिक ढंग के थे।
यह क़ानून लगातार विकसित होता रहा। और कई बार लिखा गया। इस क़ानून के एक महत्वपूर्ण संकलन का उदाहरण वह क़ानून है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बहुत बचपन के ज़माने में संकलित किया गया। सम्भवत: जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जन्म को कुछ वर्ष हुए होंगे। उस समय एक रोमी शासक जस्टीनियन (Justinian) ने ये आदेश नए सिरे से संकलित कराए थे। इन सब क़ानूनों के संग्रह को रोमन लॉ कहा जाता है। रोमन लॉ न केवल पूरे रोमी साम्राज्य में प्रचलित रहा, बल्कि उन क्षेत्रों में भी प्रचलित रहा जहाँ रोमी शासन को टेक्स देनेवाले शासक थे और जहाँ रोमी साम्राज्य के प्रभाव थे।
फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून
रोमी साम्राज्य के प्रभाव जिन-जिन देशों के क़ानूनों पर पड़े और जिन क्षेत्रों में प्रचलित थे, वह एक लम्बी चर्चा का विषय है। लेकिन रोम का क़ानून और रोमी साम्राज्य के प्रभाव का महत्व फ़िक़्हे-इस्लामी के छात्रों के लिए एक दृष्टि से यों पैदा हो जाता है कि बहुत-से पश्चिमी प्राच्यविदों ने आज से लगभग डेढ़ पौने दो सौ वर्ष पहले यह दावा किया कि फ़िक़्हे-इस्लामी रोमी क़ानून से उद्धृत है। ऐसा मालूम होता है कि जब उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी के संग्रह का अध्ययन किया और यह देखा कि इतनी विस्तृत फ़िक़्ह, इतनी संगठित, इतनी गहरी और इतनी साइंटिफ़िक क़ानूनी व्यवस्था मुसलमानों के पास मौजूद रही है, तो शायद उनके शासकीय स्वाभिमान ने यह गवारा नहीं किया कि मुसलमानों की इस महानता को स्वीकार करें। उनके साम्राज्यवादी स्वभाव और ज़ेहन ने यह बात स्वीकार नहीं की कि मुसलमान फ़ुक़हा के इस कारनामे को स्वीकार करें। अत: उन्होंने यह निराधार दावा शुरू कर दिया कि इस्लाम का क़ानून रोमी क़ानून से उद्धृत है। उनके इस दावे की पुष्टि या खंडन करने के लिए इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने रोमी क़ानून का अध्ययन शुरू किया। पिछली सदी में बड़ी संख्या में इस्लामी विद्वानों ने रोमन लॉ का अध्ययन किया और शोध से यह साबित किया कि रोमन लॉ का इस्लामी क़ानून के विकास पर ज़र्रा-बराबर प्रभाव नहीं है। वे तमाम सुबूत और दावे जो रोमन लॉ के प्रभाव के बारे में किए गए थे और किए जाते रहे, वे सब-के-सब निराधार और ग़लत थे। रोमन लॉ का संकलन, उसके मूल विषय, उसके आदेश और मूल धारणाएँ, यह सब-के-सब फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन, विषयों और मौलिक धारणाओं के साथ हर दृष्टि से टकराते हैं। फ़िक़्हे-इस्लामी के मूल विषय क्या हैं, उनपर आगे चलकर चर्चा होगी। लेकिन रोमन लॉ के मूल विषय तीन थे।
- इस क़ानून में सबसे पहले यह बताया गया है कि व्यक्तियों (Persons) का क़ानून क्या है।
- फिर ये बताते हैं कि चीज़ों यानी Things और प्रॉपर्टी का क़ानून क्या है।
- फिर वे Actions यानी आमाल का क़ानून बनाते हैं।
यानी व्यक्ति, चीज़ें और कर्म। इन तीन विभागों में उन्होंने रोमन लॉ को विभाजित किया है। व्यक्तियों के तहत नागरिकों और अजनबियों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों पर बहस होती है। ख़ानदान और निकाह के मामलों का उल्लेख होता है। ग़ुलामी और गार्जियनशिप के मामलात बयान होते हैं। वस्तुओं के अन्तर्गत सम्पत्ति, अधिकार, क़ब्ज़ा और स्वामित्व आदि के मामलों से बहस होती है। जबकि कर्मों और ज़िम्मेदारियों के मामले में अनुबन्ध, अपराधों, उत्तराधिकार, निर्देश और वसीयत जैसे मामले शामिल हैं। आप फ़िक़्हे-इस्लामी की कोई किताब उठाकर देखिए। प्राचीन अथवा आधुनिक, वह इमाम शाफ़िई (रह॰) की किताब ‘अल-उम्म’ या इमाम मालिक की ‘मुवत्ता’ हो या आज के किसी फ़क़ीह की कोई किताब हो, उदाहरणार्थ शैख़ वहबा अज़-ज़ुहैली की ‘अल-फ़क़्हुल-इस्लामी व अदिल्लत:’ हो, या कोई और फ़तवों का सामयिक संग्रह, आपको फ़िक़्हे-इस्लामी की कोई भी किताब इन तीन शीर्षकों के तहत संकलित नज़र नहीं आएगी। इसलिए यह आधार ही ग़लत साबित हो जाता है और आरम्भ ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फ़िक़्हे-इस्लामी का सारा आरम्भ और विकास केवल क़ुरआन और सुन्नत के आधार पर और इस्लामी फ़ुक़हा की गहरी समझ की रौशनी में हुआ। इसका कोई सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोमन लॉ से नहीं रहा।
रोमन लॉ के मूल स्रोत भी फ़िक़्हे-इस्लामी के मूल स्रोतों से बिलकुल भिन्न हैं। यानी बादशाहों का दिया हुआ संकलित क़ानून मजिस्ट्रेटों के दिए हुए फ़ैसले और बादशाहों के नियुक्त किए हुए क़ानून विशेषज्ञों के फ़ैसले और मश्वरे, यह रोमन लॉ के मूल स्रोत हैं। फ़िक़्हे-इस्लामी में उनमें से कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती। फ़िक़्हे-इस्लामी न तो किसी बादशाह का दिया हुआ क़ानून है, न यह किसी मजिस्ट्रेट के दिए हुए अनुशासन हैं, न यह बादशाहों के निर्धारित किए हुए किसी सलाहकार के सुझाव हैं। किसी बादशाह या किसी शासक का फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन में कभी भी कोई हिस्सा नहीं रहा। इसपर हम आगे चलकर बात करेंगे।
फ़िक़्हे-इस्लामी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में थोड़ी देर के लिए भी यह माना जा सके कि यह रोमी क़ानून से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्धृत थी। फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून दोनों की सरसरी जानकारी रखनेवाला विद्यार्थी भी यह बात नोट किए बिना नहीं रह सकता कि इन दोनों व्यवस्थाओं में धारणाओं का मौलिक मतभेद मौजूद है। रोमी क़ानून के कुछ मौलिक आदेश इस्लाम की मूल शिक्षाओं से टकराते हैं। इस क़ानून के कुछ आदेश ऐसे हैं जो इस्लाम की न्याय की धारणा के ख़िलाफ़ हैं। यह आदेश न केवल इस्लाम की न्याय की धारणा के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि दुनिया की कोई भी सुसंस्कृत व्यवस्था इन धारणाओं को आज स्वीकार नहीं करती। स्वयं रोम में वे धारणाएँ आज अस्वीकार्य हैं। उदाहरण के रूप में उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई क़र्ज़दार व्यक्ति क़र्ज़ अदा न कर सके तो उसे क़त्ल कर दिया जाए। और अगर क़र्ज़ की रक़म थोड़ी हो तो क़र्ज़दार को क़र्ज़ देनेवाले का ग़ुलाम बना दिया जाए। यह बात आज का या अतीत का कोई भी न्यायप्रिय इंसान स्वीकार नहीं कर सकता।
इसके बावजूद उन्नीसवीं सदी में जब पश्चिमी शोधकर्ताओं ने यह बात देखी कि फ़िक़्हे-इस्लामी दुनिया के इतिहास की सबसे संगठित, सबसे संकलित और सबसे विस्तृत क़ानूनी व्यवस्था है तो शायद यह बात उनको पसंद नहीं आई। शायद उनकी साम्राज्यवादी आत्ममुग्धता ने यह गवारा नहीं किया कि किसी ग़ैर-यूरोपीय और ग़ैर-मसीही सभ्यता की महानता का कोई पहलू स्वीकार करें। उन्होंने यह दावा शुरू कर दिया कि इस्लामी क़ानून रोमन लॉ से उद्धृत है। उन्नीसवीं सदी के मध्य से कुछ लोगों ने यह दावे करने शुरू कर दिए थे। और उन दावों के आधार पर किताबें और लेख लिखे जाने लगे थे। मुसलमानों में कमज़ोर ईमान रखनेवाले कुछ लोगों को या शरीअत का ज्ञान न रखनेवाले कुछ पश्चिमी क़ानूनविदों को यह बात समझा दी गई कि फ़िक़्हे-इस्लामी का सारा संग्रह रोमी क़ानून से उद्धृत है।
फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून की परस्पर साझी विशेषताएँ
यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि जो लोग फ़िक़्हे-इस्लामी को रोमी क़ानून से उद्धृत या प्रभावित बताते थे वे सब-के-सब बदनीयत या दुराग्रही न थे। सम्भव है कि उनमें से कुछ लोगों को सचुमच ऐतिहासिक या ज्ञानपरक तथ्यों को समझने में भ्रम हुआ हो और वे नेक नीयती से यही समझने लगे हों कि फ़िक़्हे-इस्लामी का कम-से-कम आरम्भिक भाग दो तीन सदियों का संग्रह रोमी क़ानून से उद्धृत है। अगर ऐसा हो तो इस ग़लतफ़हमी की वजह कुछ ऐसी साझी धारणाएँ और मिलते-जुलते सिद्धान्त हो सकते हैं जो रोमी क़ानून और फ़िक़्हे-इस्लामी दोनों में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में दोनों क़ानूनों का आरम्भ सीमित लिखित स्पष्ट आदेशों से हुआ। फ़िक़्हे-इस्लामी का सारा आधार पवित्र क़ुरआन, विशेषकर उसके आदेशों से सम्बन्धित आयतों और हदीसों, विशेषकर आदेशों से सम्बन्धित हदीसों पर है। इन सारे फ़िक़ही आदेशों की संख्या कुछ हज़ार से ज़्यादा नहीं। यही हाल रोमी क़ानून का है। जैसा कि अभी बताया गया कि रोमी क़ानून का बाक़ायदा आरम्भ इन बारह तख़्तियों से हुआ जो 450 ईसा पूर्व में लिखी गई थीं।
फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून में समानता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन दोनों का विकास अधिकतर फुक़हा और क़ानूनविदों की व्याख्याओं से हुआ। फ़िक़्हे-इस्लामी तो कहना चाहिए कि तमाम-तर ही फ़ुक़हा के इजतिहादात (क़ुरआन एवं हदीस के गूढ़ अध्ययन एवं चिन्तन से प्राप्त रायों) और फ़तवों पर निर्भर है। रोमी क़ानून में भी क़ानूनविदों का हिस्सा ख़ासा महत्वपूर्ण है। रोमी क़ानून एवं न्याय के उदाहरणों में क़ानून विशेषज्ञ यानी prudents जिनकी नियुक्ति बादशाह किया करता था, आम लोगों के लिए क़ानून की व्याख्या का कर्तव्य निभाया करते थे। वास्तव में यह विशेषज्ञ या सरकारी क़ानून व्याख्याता बादशाह के प्रवक्ता होते थे जो बादशाह की तरफ़ से क़ानून की व्याख्या करने पर नियुक्त थे। रोमन लॉ के विकास में इन विशेषज्ञों की व्याख्याओं का ख़ासा हिस्सा है। रोमी क़ानून का यह भाग शाब्दिक रूप से Responsa Prudentium यानी विशेषज्ञों का उत्तर कहलाता है। इस हिस्से को हम आंशिक समानता के आधार पर फ़िक़्हे-इस्लामी के फ़तवों के संग्रह के समान क़रार दे सकते हैं।
तीसरी महत्वपूर्ण समानता दोनों व्यवस्थाओं के बीच यह है कि दोनों के यहाँ उन आरम्भिक स्पष्ट आदेशों को एक सम्मान और श्रद्धा का दर्जा प्राप्त था जिनसे आरम्भ हुआ था। फ़िक़्हे-इस्लामी में तो इसलिए कि इन आरम्भिक स्पष्ट आदेशों, यानी आदेशों से सम्बन्धित आयतों और आदोशों से सम्बन्धित हदीसों का आधार अल्लाह की उतारी हुई वह्य (प्रकाशना) पर है और यह स्पष्ट आदेश सृष्टि के रचयिता की इच्छा को दर्शाते हैं। रोमी क़ानून में बारह तख़्तियाँ और बाद में किसी हद तक संकलित जस्टीनियन को जो सम्मान प्राप्त हुआ वह इन स्पष्ट आदेशों की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के आधार पर प्राप्त हुआ।
चौथी महत्वपूर्ण समानता दोनों के बीच यह नज़र आती है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को बहुत जल्द वैश्विक व्यवस्था की हैसियत प्राप्त हो गई। रोमी क़ानून आगे चलकर रोमी साम्राज्य से बाहर भी लोकप्रिय हुआ। फिर जब रोमी साम्राज्य मसीहियत का केन्द्र बना और पश्चिमी रोमी साम्राज्य अस्तित्व में आया तो उसका क़ानून भी यही रोमी क़ानून क़रार पाया और यों यूरोप के अधिकतर हिस्से पर रोमी क़ानून के राज का सिक्का जारी हुआ। आगे चलकर जब रोमी साम्राज्य ने यूरोप से बाहर अफ़्रीक़ा और एशिया में विभिन्न इलाक़ों पर क़ब्ज़ा करके उनको अपने अधिकृत क्षेत्रों में शामिल किया तो रोमी क़ानून का एक नया विभाग अस्तित्व में आया जो ग़ैर-यूरोपीय, ग़ैर-मसीही इलाक़ों के असभ्य नागरिकों के लिए था। क़ानून के इस विभाग के लिए क़ौमों का क़ानून यानी Jus Gentium की शब्दावली अपनाई गई। इसी तरह जो क़ानूनी विभाग ग़ैर-रोमी यूरोपीय अधिकृत क्षेत्रों के लिए था वह प्रावेंशियल लॉ कहलाता था। यह विभाग रोमी साम्राज्य के इन प्रान्तों या इलाक़ों में कार्यरत था जो रोम से बाहर विशेषकर पूर्व यूनानी अधिकृत क्षेत्रों में क़ायम थे।
रोमी क़ानून को रोम से निकलकर यूरोप के विभिन्न स्थानों तक फैलने और फिर अफ़्रीक़ा और एशिया में अपने प्रभाव को विस्तृत करने में लगभग एक हज़ार वर्ष लगे। इसके विपरीत फ़िक़्हे-इस्लामी नव्वे वर्ष के अंदर-अंदर तीनों महाद्वीपों में न केवल पहुँच चुका था, बल्कि वहाँ प्रभावकारी और ताक़तवर क़ानूनी व्यवस्था की हैसियत से लागू हो चुका था।
सम्भवत: इन सीमित और आम अंदाज़ की कुछ समानताओं और कुछ आंशिक आदेशों की समानता के आधार पर कुछ लोगों ने यह समझा कि फ़िक़्हे-इस्लामी रोमी क़ानून से उद्धृत है। अगरचे इस प्रकार के आरम्भिक अस्पष्ट दावे तो अठारवीं सदी के आरम्भ से ही किए जाने लगे थे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर-शोर से यह बात उन्नीसवीं सदी के मध्य से कही गई। इन दावों के समर्थन में जो तर्क दिए गए वे इस प्रकार के थे।
- पवित्र क़ुरआन में क़ानूनी आदेश ज़्यादा नहीं हैं। पवित्र क़ुरआन की कुछ सौ आदोशों से सम्बन्धित आयतों से इतना विस्तृत फ़िक़ही संग्रह कैसे निकाला जा सकता है। हो न हो यह सारा संग्रह रोमी क़ानून ही से लिया गया होगा। जब मुसलमानों ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के दौर में सीरिया के इलाक़े फ़त्ह किए तो वहाँ रोमी क़ानून के प्रभाव मौजूद थे। वहीं से ताबिईन फ़ुक़हा ने यह प्रभाव लिए और उनको बाक़ायदा क़ानूनी धारणाओं की शक्ल दे दी।
- कुछ मौलिक क़ानूनी सिद्धान्तों को धार्मिक श्रद्धा देने के लिए हदीस का नाम दे दिया गया और उनको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से जोड़ दिया गया। याद रहे कि उन्नीसवीं सदी का मध्य ही वह ज़माना है जब पश्चिमी प्राच्यविदों ने हदीस संकलन के बारे में झूठ बोलने का कुत्सित सिलसिला शुरू किया था।
- रोमी क़ानून और रोमी धारणाओं से लाभान्वित हुए बिना इस्लामी क़ानून इतनी तेज़ी से विकास न कर सकता था। यह अद्वितीय विस्तार और यह अद्वितीय तेज़ रफ़्तारी इस बात का प्रमाण है कि मुसलमान फुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने किसी उपलब्ध विकसित क़ानून से लाभ उठाया था, जो ज़ाहिर है कि रोमी क़ानून ही हो सकता था जो सीरिया के विजित क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध था।
उन्नीसवीं सदी की आख़िरी चौथाई में और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में यह बात और अधिक ज़ोर-शोर से दोहराई गई। फ़ॉन क्रेमर, डी बोयर, गोल्ड तसेहर और आख़िर में जोज़फ़ शख़्त ने इस विषय पर लेखों के अंबार लगा दिए। यह अजीब संयोग है कि यह दावा करने में रोम के मूल निवासियों या इटली के प्राच्यविदों की तुलना में जर्मन, विशेषकर यहूदी प्राच्यविद ज़्यादा आगे-आगे थे। उन लोगों ने यह आवाज़ इतनी शिद्दत से बुलंद की कि पश्चिमी जगत् तो पश्चिमी जगत्, स्वयं मुस्लिम जगत् के बहुत-से लोग इससे प्रभावित हुए बिना न रह सके।
इन लोगों के ‘तर्क’ भी लगभग वही थे, यानी चूँकि सीरिया और इराक़ सभ्य स्थान थे। वहाँ यह क़ानून पहले से प्रचलित थे। इसलिए इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) का उनसे प्रभावित होना अपरिहार्य था। या यह कि दिन-प्रतिदिन राज्य और समाज की समस्याओं का समाधान चूँकि शरीअत (क़ुरआन और सुन्नत) मैं मौजूद न था, इसलिए न केवल शासक, बल्कि न्यायाधीश और फ़ुक़हा मजबूर थे कि सीरिया और इराक़ के विजित इलाक़ों में प्रचलित स्थानीय रिवाजों और प्रचलित क़ानूनी धारणाओं के अनुसार नित-नए सामने आनेवाले मामलात का फ़ैसला करें। हमें पश्चिमी विद्वानों और प्राच्यविदों से तो कोई शिकायत नहीं। शिकायत ग़ैरों से नहीं, अपनों से होती है। अपनों में से जब कुछ लोग इन कमज़ोर और अधकचरी बातों को दोहराते हैं तो दुख होता है।
फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून के बीच अन्तर
सच तो यह है कि फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून के बीच अन्तर और भिन्नता इतनी गहरी और इतनी बड़ी है कि उनमें से एक को दूसरे से उद्धृत या प्रभावित क़रार देना मौलिक रूप से ग़लत है। फ़िक़्हे-इस्लामी व्यापक परिवर्तन और मानव-जीवन के भरपूर परिवर्तन का प्रवक्ता है। इसके विपरीत रोमी क़ानून पूर्व जीवन-शैली ही के ज़रा बेहतर सुधार का आवाहक है। फ़िक़्हे-इस्लामी में स्वतंत्र रूप से क़ानून बनाने का दायरा बहुत सीमित है। यहाँ मौलिक क़ानूनी धारणाएँ पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल में तय कर दी गई हैं। अब शेष क़ानून बनाने का काम रहती दुनिया तक के लिए उन्हीं सीमाओं के अंदर रहकर होगा जो क़ुरआन और सुन्नत ने तय कर दी हैं। दूसरी तरफ़ रोमी क़ानून में स्वतंत्र रूप से क़ानून बनाने का दायरा असीमित है। फ़िक़्हे-इस्लामी में क़ानून बनाना तमाम-तर फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन (क़ुरआन एवं हदीस का गहन अध्ययन कर उनकी रौशनी में नए-नए मामलों का समाधान सुझानेवालों) के स्वतंत्र रूप से इजतिहाद (राय) के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है, जबकि रोमी क़ानून लगभग सारे-का-सारा या तो बादशाह का प्रदान किया हुआ है या फिर बादशाहों के नियुक्त किए हुए विशेषज्ञों का निर्धारित किया हुआ है। फिर फ़िक़्हे-इस्लामी मूलत: एक असंकलित क़ानून है, जबकि रोमन क़ानून की विशेषता ही यह बताई जाती है कि वह सभ्य दुनिया का पहला संकलित क़ानून है। इन मौलिक और सैद्धान्तिक बातों के अलावा बहुत-से आंशिक आदेश ऐसे हैं जहाँ दोनों व्यवस्थाओं में मौलिक अन्तर पाया जाता है। यह अन्तर मात्र आदेश का नहीं, बल्कि उनके पीछे कार्यरत धारणाओं और मूल नियमों एवं सिद्धान्तों का अन्तर है। उदाहरण के रूप में महिलाओं के मामले में फ़िक़्हे-इस्लामी में हर वयस्क पुरुष और स्त्री को समान नागरिक और दीवानी अधिकार प्राप्त हैं। वे अपने निजी और व्यक्तिगत मामलों, सम्पत्ति और मिल्कियत की प्राप्ति और इसके प्रबन्धन तथा बरतने में बिलकुल आज़ाद हैं। इसके विपरीत रोमी क़ानून में महिलाएँ स्थायी रूप से पुरुषों की निगरानी और संरक्षण में थीं। वे अपने निगराँ या संरक्षक की अनुमति के बिना न कोई सम्पत्ति प्राप्त कर सकती थीं और न प्राप्त सम्पत्ति में किसी उपभोग की अधिकारी थीं। यह प्रतिबंध महिलाओं पर जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक रहता था।
फ़िक़्हे-इस्लामी के आदेश के अनुसार मह्र पति के ज़िम्मे होता है जो उसको अनिवार्य रूप से चुकाना पड़ता है। रोमी क़ानून में मह्र पत्नी चुकाती थी। फ़िक़्हे-इस्लामी में लेपालक (दत्तक) पुत्र अस्ल बेटे की जगह नहीं ले सकता, न लेपालक पर अस्ल बेटे के आदेश जारी हो सकते हैं, जबकि रोमी क़ानून और उससे प्रभावित तमाम पश्चिमी क़ानूनों में लेपालक के वही आदेश हैं जो सगी सन्तान के होते हैं।
फिर फ़िक़्हे-इस्लामी में सादगी और क़ानून की रूह और उद्देश्य पर अस्ल ज़ोर है। तक़्वा लिल्लाहियत (अल्लाह के लिए निष्ठा) और आध्यात्मिक पाकीज़गी क़ानून का पालन करने का मूल उद्देश्य है। जबकि रोमी क़ानून अपने स्वभाव के दृष्टि से अधार्मिक और ग़ैर-आध्यात्मिक क़ानून है। वहाँ सारा ज़ोर बाह्य रूप और दिखावे पर है। यहाँ अस्ल ज़ोर नीयत और उसके फल पर है।
विरासत के आदेश शरीअत में बिलकुल भिन्न प्रकार के हैं। रोमन लॉ, बल्कि तमाम पश्चिमी क़ानूनों में प्रचलित विरासत के आदेश फ़िक़्हे-इस्लामी के विरासत के आदेशों से मूल रूप से भिन्न हैं।
इसके अलावा फ़िक़्हे-इस्लामी ने बहुत-सी ऐसी नई धारणाएँ दुनिया को दीं जिनसे रोमन लॉ तो क्या, आधुनिक काल के बहुत-से विकसित क़ानून भी लम्बे समय तक अनभिज्ञ रहे। क़ानून के सिद्धान्त, क़ानून की व्याख्या के सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून, संवैधानिक क़ानून आदि क़ानून के वे विभाग हैं जिनसे रोमी क़ानून बहुत बाद में परिचित हुआ। वहाँ न वक़्फ़ की कोई परिकल्पना थी और न ‘शुफ़आ’ (वह अधिकार जो घर या ज़मीन के पड़ोस से प्राप्त होता है) का, बल्कि आज भी फ़िक़्हे-इस्लामी के अनेक विभाग ऐसे मौजूद हैं जिनके जैसा पश्चिमी क़ानूनों में मौजूद नहीं। उदाहरण के रूप में ‘इल्मे-फ़ुरूक़’ और ‘इल्मे-इश्बाह’ और ‘इल्मे-नज़ाइर’ का नाम लिया जा सकता है।
रोमी क़ानून से फुक़हा की लापरवाही
फ़िक़्हे-इस्लामी और रोमी क़ानून की तुलना पर यह बातें जो ज़रा लम्बी हो गईं, यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं कि फ़िक़्हे-इस्लामी एक बाक़ायदा अपने आपमें क़ानूनी-व्यवस्था है, जो अपने विकास में किसी तरह भी रोमी क़ानून पर निर्भर नहीं। यही वजह है कि ‘तारीख़’ (इतिहास) और ‘तज़किरा’ की किसी भी पुरानी या नई किताब में इस बात का हल्का-सा भी कोई इशारा नहीं मिलता कि किसी फ़क़ीह या ग़ैर-फ़क़ीह लेखक ने रोमी या बाज़न्तीनी क़ानूनों से दिलचस्पी ली हो, उनका अध्ययन क्या हो या उनसे आंशिक जानकारी प्राप्त की हो।
इसके अलावा अक्सर फ़िक़ही मसलक कूफ़ा, बस्रा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा या आगे चलकर बग़दाद में पैदा हुए जो विशुद्ध इस्लामी आबादियाँ थीं। इन इस्लामी बस्तियों में न रोमी प्रभाव पाए जा सकते थे न बाज़न्तीनी। आख़िर मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक (रह॰) और उनके उस्ताद इमाम नाफ़े और अबू-ज़न्नाद ने किस तरह और किन स्रोतों से रोमी क़ानून की धारणाओं से जानकारी प्राप्त की। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने मक्का मुकर्रमा में जब फ़िक़्ह में उनकी गहरी सूझ-बूझ परिपक्व हो रही थी, किस प्रकार रोमी क़ानून तक पहुँच बनाई? यही सवाल शेष फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन के बारे में किया जा सकता है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि फ़िक़्हे-हनफ़ी का अधिकतर विकास मावराउन्नहर और इराक़े-अजम के इलाक़ों में हुआ जो रोमी प्रभाव से बाहर थे।
इसके अलावा यह हक़ीक़त भी अत्यन्त महत्व रखती है कि न केवल फ़िक़्हे-इस्लामी के गठन के समय, यानी आरम्भिक चार हिजरी सदियों में, बल्कि बाद में लगभग और आठ सौ वर्ष तक मुसलमानों ने क़ानून की किसी किताब का अरबी में अनुवाद नहीं किया। न केवल रोमन भाषा से, बल्कि पश्चिम और पूरब की किसी भाषा से भी क़ानून की किसी किताब का अरबी में अनुवाद नहीं किया गया।
अगर आपने इस्लाम के इतिहास में यूनानियों के ज्ञान-विज्ञान के अनुवाद का विवरण पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने यूनानियों के ज्ञान-विज्ञान की बहुत-सी किताबें अरबी में अनुवाद कीं। अफ़लातून और अरस्तू की किताबें अरबी में अनुवाद हुईं। सुक़रात, बुक्ऱात और हकीम जालीनूस की किताबें अनुवाद हुईं। मंतिक़ (तर्कशास्त्र), फ़लसफ़ा (दर्शन) और तिब्ब (चिकित्सा पद्धति) पर सैंकड़ों बल्कि शायद हज़ारों किताबें विभिन्न भाषाओं से अरबी में अनुवाद हुईं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि क़ानून या संविधान के विषय पर कोई भी किताब अरबी भाषा में अनुवाद हुई हो। पहली सदी हिजरी से लेकर ग्यारहवीं बारहवीं सदी हिजरी तक एक उदाहरण भी ऐसा नहीं मिलता कि क़ानून की कोई किताब अरबी में अनुवाद करने की आवश्यकता महसूस की गई हो। इसकी वजह केवल यह है कि इस्लाम का क़ानून और फ़िक़्ह उतना संकलित और संगठित था कि मुसलमानों ने एक पल के लिए भी यह आवश्यकता महसूस नहीं की कि उनको किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो क़ानून के मैदान से सम्बन्ध रखती हो और दुनिया की किसी दूसरी क़ौम के पास मौजूद हो।
जो बात रोमी क़ानून के बारे में कही गई वही बात दुनिया के दूसरे क़ानूनों के बारे में भी कही जा सकती है। प्राचीन क़ानूनों में रोमी क़ानून तुलनात्मक रूप से ज़्यादा संकलित और सख़्त-जान था। रोमी क़ानून ही के ध्वजावाहक शायद ऐसा दुस्साहस कर सकते थे कि ऐसा निराधार और कमज़ोर दावा करें जो शोध के तराज़ू में इतना हल्का साबित हो। दूसरी क़ौमों ने ऐसा दावा नहीं किया। हिंदुओं ने तो कभी इस बात का कोई गम्भीर दावा नहीं किया कि मुसलमानों ने कोई उल्लेखनीय चीज़ उनसे ली है। यहूदियों के पास अगरचे एक संकलित और संगठित क़ानून प्राचीन काल से चला आ रहा है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि फ़िक़्हे-इस्लामी उनके संग्रहों से उद्धृत है। पवित्र क़ुरआन की तरफ़ से उनकी शरीअत के आसमानी शरीअत होने को स्वीकार किए जाने के बावजूद यहूदी विद्वानों ने, कभी ऐसा दावा नहीं किया। बौद्धों के पास तो सिरे से कोई क़ानून ही नहीं था। उन्होंने नैतिक आचरण को ही काफ़ी समझा। ईसाइयों ने ख़ुद से तौरात के क़ानून को निरस्त ठहराकर कुछ नैतिक नारों को काफ़ी समझ लिया। उनको यह दावा करने की आवश्यकता ही न पड़ी कि फ़िक़्हे-इस्लामी उनके विचारों से उद्धृत है। इसलिए इन उदाहरणों के बाद हम पूरे विश्वास से निस्संकोच यह दावा स्वीकार कर सकते हैं कि फ़िक़्हे-इस्लामी तमाम-तर सौ प्रतिशत पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सिद्धान्तों पर क़ायम है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) को जो इजतिहादी सूझ-बूझ अल्लाह तआला ने प्रदान की थी, फ़िक़्हे-इस्लामी के पूरा विस्तारण इसपर आधारित है। और इसका सारा-का-सारा विकास इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों), क़ुरआन के टीकाकार और हदीस के व्याख्याताओं पर निर्भर है।
मुसलमानों का जिन क़ौमों से क़रीबी वास्ता रहा, उदाहरणार्थ यहूदी और ईसाई, उनके भी किसी ज़िम्मेदार विद्वान ने अपनी किसी धार्मिक अवधारणा या अक़ीदे के फ़िक़्हे-इस्लामी पर प्रभावी होने का दावा नहीं किया। ईसाइयों के यहाँ तो सिरे से कोई क़ानून ही नहीं था। ईसाइयत के तो पहले दिन से ही तौरात के क़ानून को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन यहूदियों के यहाँ एक संकलित क़ानून लिखा हुआ मौजूद था। इसपर किताबें भी मौजूद थीं और स्वयं मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का मदरसा यानी दर्सगाह मौजूद थी, जहाँ यहूदी क़ानून की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन न यहूदियों ने इसका दावा किया कि फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन में उनके मदरसों का कोई दख़ल है, न मुसलमानों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि यहूदियों से भी उनके क़ानून के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाए।
क़ानून का वास्तविक एवं अन्तिम स्रोत
आगे बढ़ने से पहले एक मौलिक सवाल का जवाब आवश्यक है जिससे फ़िक़्हे-इस्लामी के मौलिक आधार को समझने में सहायता मिलती है। वह यह है कि मानव-जीवन का जो नियम संकलित किया जाए, वह चाहे किसी एक विभाग को संगठित करता हो या एक से अधिक विभागों को संगठित करता जो, उसका आख़िरी प्रमाण, यानी वैचारिक आधार क्या होगा। कुछ लोगों का ख़याल है कि इस नियम का मूलाधार मानव बुद्धि को होना चाहिए। इंसान अपनी बुद्धि से यह फ़ैसला करे कि उसके और दूसरे इंसानों के जीवन को कैसे संगठित किया जाए। इस्लाम और अन्य आसमानी शरीअतों का कहना यह है कि यह चीज़ केवल अल्लाह की वह्य के आधार पर ही संकलित की जा सकती है। इसलिए कि न तो इंसानों में बुद्धि के आधार पर कोई चीज़ एक जैसी बन सकती है, न कोई इंसान अपने निजी हितों और निजी निहतार्थों से परे हो सकता है, न कोई इंसान अपने विशेष परिवेश से मुक्त होकर, केवल नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर या केवल बौद्धिक अपेक्षाओं के आधार पर कोई चीज़ तय कर सकता है। इसलिए जब भी इंसानों की बुद्धि को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसमें निजी स्वार्थ और निजी निहितार्थ का आ जाना अपरिहार्य है।
यह केवल अल्लाह की वह्य (प्रकाशना) है जो तमाम इंसानों के हितों और निहितार्थों से ऊपर होती है।
अल्लामा इक़बाल ने फ़रमाया है कि केवल वह्य सत्य है जो हर इंसान के कल्याण और सफलता का ख़याल रखती है, और उसकी निगाह में हर इंसान का कल्याण बराबर और समान महत्व रखता है। इसके मुक़ाबले में जब मानव-बुद्धि को यह ज़िम्मेदारी दी जाएगी तो या तो उन मामलों का फ़ैसला अपने अनुभव के आधार पर करेगी, या अनुमान एवं तर्क के आधार पर करेगी। अनुभव और अनुमान तथा तर्कों के अलावा मानव-बुद्धि के पास और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे काम लेकर वह इंसानों के लिए कोई व्यवस्था बना सके। अनुभव हर इंसान का सीमित होता है। किसी इंसान का अनुभव इतना असीमित नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में बैठकर चीनियों के लिए व्यवस्था बना दें, या कोई चीनी बीजिंग में बैठकर हमारे लिए व्यवस्था बना दे। आज हमारे लिए यह सम्भव नहीं कि हममें से कोई व्यक्ति आज से पाँच सौ वर्ष बाद में आनेवालों के लिए कोई व्यवस्था बना दे। किसी इंसान का अनुभव असीमित नहीं होता। अत: एक अत्यन्त सीमित अनुभव की रौशनी में असीमित इंसानों के असीमित मामलों के लिए व्यवस्था बनाई ही नहीं जा सकती। यही हाल अनुमान का है कि इंसान किसी देखी हुई चीज़ पर अनदेखी चीज़ों का अनुमान करता है। एक चीज़ आपने देखी और उसपर एक दूसरी अनदेखी चीज़ को अनुमानित करके एक अनुमान मालूम कर लिया। जो दो या चार या पाँच चीज़ें आपने देखी हैं उनपर उन हज़ारों, बल्कि लाखों और करोड़ों चीज़ों को अनुमान नहीं किया जा सकता जो हमारे देखने में नहीं आईं। फिर अगर यह बुद्धि व्यक्ति की है तो मामला और भी ख़तरनाक हो जाता है। एक व्यक्ति की बुद्धि पर भरोसा करके जिन लोगों ने मामलात चलाए उनका अंजाम दुनिया के सामने है। अगर एक से अधिक व्यक्तियों को अनुमान एवं तर्क के आधार पर व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी दी जाए तो भी दुनिया का अनुभव हमारे सामने है कि वह अपने निजी हितों से ऊपर नहीं उठ सकते। जिस वर्ग से उस गिरोह का सम्बन्ध होगा उस वर्ग के हितों को वह सामने रखेगा और जिस वर्ग से सम्बन्ध नहीं होगा इस वर्ग का हित प्रभावित हो जाएगा। हम सबका सम्बन्ध पढ़ने-पढ़ाने के मामलों से है। अगर अध्यापक और छात्रों को देश की व्यवस्था बनाने की अनुमति दे दी जाए तो इस व्यवस्था में सारा हित अध्यापकों और छात्रों ही का होगा और मज़दूरों, किसानों, पूँजीपतियों, कारख़ानेदारों और कर्मचारियों, सबका हित प्रभावित हो जाएगा। कर्मचारियों को यह अधिकार दिया जाए तो शेष सब का हित प्रभावित हो जाएगा और उनका अपना हित पूरा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की शरीअत ने यह तय किया कि किसी भी व्यवस्था में, और मानव-जीवन के किसी भी ढंग में जो-जो चीज़ें ज़रूरी और मूल स्थान रखती हैं उनके वे मौलिक आधार और उनके वे मौलिक आदेश अल्लाह की वह्य के ज़रिये तय कर दिए जाएँ। जहाँ बुद्धि के भटकने की सम्भावना है। जहाँ मानव-बुद्धि के बारे में इस बात की सम्भावना है कि वह किसी ख़ास वर्ग या व्यक्ति के हितों को सामने रखेगी वहाँ अल्लाह की वह्य ने वे मौलिक धारणाएँ उपलब्ध कर दीं। अच्छाई और बुराई का मापदंड तय कर दिया कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। एक बार जब यह मौलिक ढाँचा तय हो जाए कि क्या ‘ख़ैर’ है और क्या ‘शर’ है, और यह कि सत्य-असत्य का आख़िरी पैमाना क्या है तो फिर हमेशा-हमेशा के लिए इन सीमाओं के अंदर मानव-बुद्धि को अनुमति है कि वह जितना विस्तृत विवरण चाहे तय कर ले। वह विवरण जो किसी व्यक्ति या गिरोह की बुद्धि तय करेगा अगर क़ुरआन और सुन्नत के इन मौलिक आदेशों के अनुसार है तो स्वीकार्य है और अगर उनसे टकराता है तो अस्वीकार्य है। इन मौलिक आदेशों के अंदर अगर एक से अधिक मत पाए जाते हैं और इस ढाँचे में एक से अधिक मतों की गुंजाइश मौजूद है तो वह एक से अधिक मत भी स्वीकार्य हैं। आपमें से जिनको हदीस पर लेक्चर्स सुनने का मौक़ा मिला है उनको याद होगा कि मैंने उदाहरण दिए थे कि किस तरह एक हदीस के एक से अधिक भावार्थ सहाबा, ताबिईन और फ़ुक़हा ने अपनी अपनी समझ और अपने ज्ञान के अनुसार समझे, और वे सारे के सारे भावार्थ तर्क के आधार पर उम्मत के विद्वानों एवं चिन्तकों के विभिन्न वर्गों ने स्वीकार किए। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं कि सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने क़ुरआन के एक स्पष्ट आदेश या हदीस के एक से अधिक भावार्थ समझे और वे विभिन्न भावार्थ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़बान से एक ही समय में दुरुस्त भी क़रार पाए। पवित्र क़ुरआन की एक आयत को एक से अधिक अंदाज़ में सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने कैसे समझा और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इन दोनों अर्थों को कैसे दुरुस्त क़रार दिया, इसके उदाहरण हदीस की किताबों में मौजूद हैं। जहाँ पवित्र क़ुरआन की किसी आयत या स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के किसी कथन का एक अर्थ ही दुरुस्त था वहाँ उन्होंने इसकी निशानदेही भी कर दी। जहाँ एक से अधिक अर्थों की गुंजाइश थी वहाँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक से अधिक व्याख्याओं की अनुमति दी। लेकिन यह अनुमति उन सीमाओं और चौखटे के अंदर दी गई जो पवित्र क़ुरआन और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत में मौजूद हैं। यह चौखटा मानव-जीवन की तमाम मौलिक समस्याओं का जवाब देता है। यह चौखटा मानव-जीवन के मौलिक निहितार्थों की रक्षा करता है। यह चौखटा कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के हितों की भी रक्षा करता है और ताक़तवर-से-क़तवर को भी क़ानून का पाबंद रखता है। यह चौखटा इंसानी नैतिक आचरण की देखभाल करता है, यह इस्लामी जीवन की निरन्तरता का ज़ामिन है, यह मानव-जीवन के वर्तमान और भविष्य को अतीत से जोड़े रखने में मौलिक भूमिका निभाता है, इस चौखटे के अंदर रहकर मानव-बुद्धि जितना सोच सके उसको सोचने की अनुमति है, मानव-बुद्धि जितनी समस्याओं की कल्पना कर सकती है और उनके जो समाधान सुझा सकती है वे समाधान सुझाने की उसको पूरी अनुमति है। लेकिन यह मौलिक मार्गदर्शन जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नत ने दे दिया, यह मौजूद न हो तो वह कुछ होता है जो आज पश्चिम में हो रहा है। आज वहाँ आए दिन धर्म और विचारधाराएँ बदलती हैं। हर आनेवाली सुबह सत्य-असत्य का एक नया मापदंड लेकर अस्तित्व में आती है। आज का पश्चिम अतीत से रिश्ता तोड़ चुका है। आज वहाँ सिवाय मुसलमानों से नफ़रत के, अतीत की शेष तमाम परम्पराएँ दम तोड़ चुकी हैं। आज वहाँ सत्य-असत्य का फ़ैसला इंसानों के भौतिक हितों के आधार पर होता है। फिर भौतिक हित कब तक जारी और निर्णायक होगा इसका आख़िरी फ़ैसला संख्या की अधिकता और शस्त्र-शक्ति पर है।
पश्चिम में आज यह तय कर लिया गया कि अमुक दल या संस्था के सदस्य, जिनकी संख्या दो सौ या तीन सौ या कुछ हज़ार है, उनकी बुद्धि जीवन के तमाम बड़े-बड़े मामलों का अन्तिम और निश्चित निर्णय कर सकती है। चुनाँचे इन इंसानों की बुद्धि ने जो फ़ैसले किए वे आज मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मेरी हया इसकी अनुमति नहीं देती कि मैं इन फ़ैसलों के उदाहणर दूँ जो इंसानों ने हमारी दुनिया की बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के इंसानों के बारे में अपनी बुद्धि और गहरी सूझ-बूझ के आधार पर किए हैं। ताज़ातरीन फ़ैसला सुन लीजिए। तुर्की (अब तुर्किये) जो मुस्लिम देश है और जिसका एक हिस्सा यूरोप में है, और लगभग तीन चौथाई से ज़्यादा हिस्सा एशिया में है, इस एक चौथाई से कम हिस्से की वजह से वह यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं और लगभग पचास वर्ष से प्रयासरत हैं कि उनको यूरोपियन यूनियन की सदस्यता प्रदान कर दी जाए। उनके नेतृत्व ने, अल्लाह तआला उनको मार्गदर्शन दे, हर वह काम किया जिसकी यूरोपीय लोगों ने उनसे माँग की कि वह यह काम भी करें और वह काम भी करें। ताज़ातरीन, जब उनका मामला तय करने के क़रीब हुआ और फ़ैसला होने लगा कि हमारे तुर्क भाई यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाने की दरख़ास्त देने के योग्य क़रार दिए जाएँ तो यूरोप के इन बुद्धिमानों ने आपत्ति की कि पिछले दिनों आपकी पार्लियामेंट में एक क़ानूनी मुसव्वदा पेश हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि बदकारी (व्यभिचार) को तुर्की में अपराध क़रार दे दिया जाए। यह चीज़ कि बदकारी को अपराध समझा जाए, यूरोपीय धारणाओं के ख़िलाफ़ है। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वह जिस तरह से चाहे अपनी इज़्ज़त और नैतिक आचरण का सौदा करे। अत: यह प्रतिबन्ध लगाना आज़ादी, समानता और लोकतंत्र के विरुद्ध है। तुर्क बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी समझ-बूझ को अन्तिम शब्द क़रार देते हुए क़ानून का वह मुसव्वदा वापस ले लिया। अफ़सोस की बात यह है कि व्यभिचार को वैध ठहराकर भी तुर्कों को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। हमारे लिहाज़ से अगरचे तुर्कों का यह क़दम दुख की बात है, लेकिन ये फ़ैसले हैं जो मानव-बुद्धि के आधार पर होते हैं जिनका नैतिक आचरण, अध्यात्म, चरित्र किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं। अगर एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि जीवन की मौलिक समस्याओं का जवाब देने का अधिकार मानव-बुद्धि को है, अल्लाह की वह्य को नहीं है, तो फिर मानव-जीवन के लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचता। एक लाख इंसान होंगे तो वह एक लाख बौद्धिक सुझाव देंगे। जहाँ एक अरब इंसान होंगे तो वह एक अरब समाधान सुझाएँगे और मानवता किसी एक समाधान तक नहीं पहुँच सकेगी।
आज मानवता को जिन असंख्य समस्याओं का सामना है और आए दिन इंसानों को जिन मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वह इसलिए है कि इंसानों ने कुछ इंसानों का यह अधिकार स्वीकार कर लिया है कि उनकी बुद्धि दुनिया के मामलों का फ़ैसला करे। अब जिसके पास डंडा है उसकी बुद्धि भी सबसे ज़्यादा बढ़कर समझी जाती है। जिसकी जेब में पैसा ज़्यादा है उसकी बुद्धि भी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। चुनाँचे आप देख लीजिए कि दुनिया में जिन क़ौमों के पास क़ुव्वत और ताक़त है उनकी व्यवस्था भी दुनिया में ज़बरदस्ती लागू की जा रही है। जिन क़ौमों के पास संसाधन ज़्यादा हैं और शक्ति के बल पर उन्होंने और भी संसाधनों पर भी क़ब्ज़ा कर लिया है, उनकी व्यवस्था दुनिया में चल रही है और लोग मानने पर मजबूर हैं। हमारे तुर्क भाइयों के दिलों में क्या है, निश्चय ही वही होगा जो मेरे और आपके दिल में है। लेकिन वे इस मजबूरी की वजह से पश्चिम के लोगों की सब शर्तें मानने पर मजबूर हैं, जिनके पास पैसा भी है और शक्ति भी और जिनकी शक्ति और पैसे की वजह से हर कोई उनके संगठन में शामिल होना चाहता है। ये वे कमज़ोरियाँ हैं जो दुनिया के क़ानूनों और व्यवस्थाओं में पाई जाती रही हैं और आगे भी पाई जाती रहेंगी।
शरीअत : एक स्पष्ट मार्ग
इसके मुक़ाबले में इस्लामी शरीअत ने जो व्यवस्था दी है, उसमें शरीअत ने एक रास्ता निर्धारित कर दिया है कि इंसान को किस रास्ते पर जाना है। इस रास्ते की मौलिक रूपरेखा और मंज़िल के निशानात अल्लाह की शरीअत ने तय कर दिए हैं। अल्लाह की शरीअत ने यह बता दिया है कि इस रास्ते पर चलोगे तो सफल रहोगे। उसके अलावा किसी और रास्ते पर चलोगे तो सफल नहीं रहोगे। अगर आपको किसी ऐसे जंगल में सफ़र करना हो जहाँ न हरियाली हो न पानी, किसी रेगिस्तान और सहरा में सफ़र करना हो और यह पता न हो कि पूरब किस तरफ़ है और पश्चिम किस तरफ़ और आपको जाना किस तरफ़ है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके लिए जगह-जगह निशान लगाकर रास्ता निर्धारित कर दे, तो आपके लिए मंज़िल पर पहुँचना आसान हो जाएगा। अब यह तय करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है और आपके अपने अधिकार में है कि आप ऊँट पर सफ़र करें, घोड़े पर सफ़र करें या गाड़ी पर सफ़र करें या साइकिल पर करें। रास्ते में रुक-रुककर जाएँ या लगातार सफ़र करें, रास्ते में ज़ादे-राह (पाथेय) क्या रखें, खाना अच्छा रखें या मामूली रखें, ये सब विवरण आपको तय करने का अधिकार है। ये सारा विवरण आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय कर सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता ही निर्धारित न हो, तो कोई कहेगा कि दाएँ चलो, कोई कहेगा कि बाएँ चलो, कोई कहेगा कि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वापस जाना चाहिए और आप बनी-इसराईल के मैदान ‘तीहा’ की तरह उसमें भटकते फिरेंगे और मंज़िल तक नहीं पहुँच सकेंगे।
इसलिए अल्लाह तआला की वह्य ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़रिये पूरी मानवता के लिए जो दयालुता-सन्देश शरीअत के रूप में भेजा वह यह है कि इस जंगल और रेगिस्तान में रास्ते की निशानदेही कर दी कि सफलता का निश्चित, आसान और सीधा रास्ता यह है जिसके दोनों ओर मंज़िल के निशानात लगे हुए हैं। यह रास्ता गंतव्य स्थान तक पहुँचा देने का ज़मानती है। इस रास्ते को अरबी भाषा में ‘शरीअत’ कहते हैं।
शरीअत एक व्यापक शब्दावली है जिसमें वे तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनकी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने शिक्षा दी है। जो कुछ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़रिये हम तक पहुँचा है वह सब का सब शरीअत है। पूरे पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के पूरे संग्रह का नाम शरीअत है। इस शरीअत में इंसान के सांसारिक और पारलौकिक जीवन की सफलताओं के लिए जिन-जिन निर्देशों और जिस-जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह सारा मार्गदर्शन का सामान इस शरीअत में मौजूद है। अरबी भाषा में शरीअत उस रास्ते को कहते हैं जिसपर चलकर आप पानी के भंडार तक पहुँच सकें। अगर आप किसी गाँव या देहात में ठहरे हों और आपके घर में पानी का स्थायी प्रबन्ध न हो तो आपको सुबह-शाम पानी लेने के लिए किसी कुँए, जलस्रोत या नहर वग़ैरा पर जाना पड़ेगा। इस चश्मे (जल स्रोत) या कुँए पर गाँव के सब लोग जा रहे होंगे। चश्मे की तरफ़ लोगों की इस लगातार आवाजाही और आने-जाने से एक रास्ता बन जाएगा जो चश्मे की तरफ़ जानेवाले दूसरे रास्तों के मुक़ाबले में छोटा होगा। कोई व्यक्ति जो पानी लेने जा रहा हो वह लंबा चक्कर लगाकर पानी के कुँए तक नहीं जाएगा, बल्कि सबसे छोटे रास्ते से जाएगा। यों वह रास्ता सीधा भी होगा, छोटा भी होगा, बहुत चौड़ा और समतल भी होगा। चूँकि पानी लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तादाद में उस ओर आ-जा रहे होंगे तो यह लोगों का आना-जाना इस बात को निश्चित बनाएगा कि आप पानी के भंडार तक पहुँच जाएँ। किसी और रास्ते से जाएँगे तो आपके भटकने की सम्भावना होगी। लेकिन इस मशहूर रास्ते पर जाएँगे तो मंज़िल तक आपका पहुँचना निश्चित होगा। ऐसे ही रास्ते को अरबी भाषा में शरीअत कहते हैं।
पवित्र क़ुरआन ने बताया है “हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया।” (क़ुरआन, 21:30) मानो जीवन के मूल स्रोतों तक जो रास्ता ले जाए वह रास्ता अरबी भाषा में शरीअत कहलाता है। यह रास्ता जो जीवन के मूल स्रोतों तक ले जाता है यह हमेशा संक्षिप्त होता है, साफ़ और सुगम होता है, चौड़ा होता है और मंज़िल तक पहुँचाने का निश्चित ज़रिया होता है। शेष कोई ज़रिया निश्चित नहीं होता। ये विशेषताएँ शब्दकोषीय अर्थ की दृष्टि से शरीअत में पाई जाती हैं।
पवित्र क़ुरआन में यह भी बताया गया कि “आख़िरत का जीवन ही वास्तव में वास्तविक जीवन है।” (क़ुरआन, 29:64) इस जीवन में सफलता की आख़िरी मंज़िल तक जो रास्ता पहुँचा दे वह शब्दावली में शरीअत कहलाता है। यह रास्ता भी अत्यन्त स्पष्ट और सीधा है, अत्यन्त सुगम और कठिनाइयों से मुक्त है। यह रुकावटों और दिक़्क़तों से भी मुक्त है और मंज़िल तक पहुँचने का एक निश्चित साधन है। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने इस मार्गदर्शन व्यवस्था और परोपकारी-सन्देश के लिए अरबी भाषा के शब्द शरीअत को अपनाया, क्योंकि यह इस अर्थ को पूरे तौर पर अदा कर देता है जो शरीअत के शब्द से अल्लाह तआला इंसानों को ज़ेहन में बिठाना चाहता है। शरीअत के रूप में जो रास्ता दिया गया है यह सांसारिक और पारलौकिक जीवन में सफलता का एक मात्र रास्ता है। यह रास्ता अत्यन्त संक्षिप्त, सीधा, सुगम, चौड़ा और मंज़िल पर पहुँचाने का एक मात्र ज़रिया है।
शरीअत का कार्यक्षेत्र
जब हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शरीअत का जायज़ा लेते हैं, यानी पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में जो शिक्षा भी उन्होंने दी है, इसका जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि शरीअत जीवन के तीन बड़े मैदानों में मार्गदर्शन उपलब्ध करती है। सबसे पहला मार्गदर्शन इंसान के मानसिक और वैचारिक मामलों के बारे में है। अगर इंसान मानसिक रूप से उलझनों का शिकार हो और मानसिक रूप से परेशान हो, उसको यह भी पता न हो कि रास्ता किधर जाता है? सफलता का रास्ता कौन-सा है और असफलता का कौन-सा, तो वह सुनसान जंगल की विशालताओं में हर ओर भटकता रहेगा और कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसलिए शरीअत ने सबसे पहला काम यह किया है कि वे आधार वास्तविक रूप से निर्धारित कर दिए जो इंसान के मानसिक रवैये का गठन करते हैं। इंसान सोचे तो किन दिशानिर्देशों पर सोचे, बौद्धिक रूप से मामलों पर ग़ौर करे तो किन सीमाओं का पाबंद हो, मौलिक सवालात क्या हैं जिनका पवित्र क़ुरआन ने जवाब दिया है, ताकि उनके आधार पर वह आगे आनेवाले सवालात के विस्तृत उत्तर दे सकें। जब आप साइंस पढ़ते हैं, उदाहरण के रूप में कैमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ मौलिक धारणाएँ और उसूल सबसे पहले बता दिए जाते हैं कि कैमिस्ट्री के मौलिक उसूल और धारणाएँ ये हैं। इन धारणाओं को जानने के बाद आप लेबारेट्री में जाएँ और जितनी मर्ज़ी जाँच-पड़ताल कर लें। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि कैमिस्ट्री की कला में शोध और प्रगति की मंज़िल बस तय करते जाएँ, और यों इसमें जितना चाहें आप आगे जाएँ। लेकिन अगर कोई अनपढ़ बूढ़ी औरत किसी गाँव और देहात से आई हो और उसको यह भी पता न हो कि कैमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। उसको आप यका-यक किसी आधुनिकतम और बेहतरीन लेबारेट्री में ले जाएँ और उससे कहें कि यहाँ बैठकर शोध करो और अमुक-अमुक महत्वपूर्ण समस्याओं को समाधान करो तो वह अनपढ़ बूढ़ी औरत वहाँ कुछ भी नहीं कर सकेगी। कभी एक चीज़ को तोड़ेगी, कभी दूसरी चीज़ को ख़राब करेगी कभी तीसरी चीज़ को बिगाड़ेगी। इसलिए कि उसको इन मौलिक चीज़ों का ही नहीं पता जिनके आधार पर शेष चीज़ों को प्रयुक्त किया जाता है।
अल्लाह तआला ने वह मौलिक सवालात बता दिए हैं जिनसे इंसान को पता चल जाता है कि इंसान को स्वयं अपनी वैचारिक कैमिस्ट्री और कायनात की इस कैमिस्ट्री को कैसे प्रयुक्त करना है। यह एक प्रयोगशाला है जहाँ आप प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर आपके सामने वे सारी मौलिक धारणाएँ और ढाँचे मौजूद हैं जो पवित्र क़ुरआन ने इस शक्ति को प्रयुक्त करने के लिए बताए हैं तो आपके लिए बहुत आसान है कि कुछ मिनटों में और कुछ लम्हों या कुछ दिनों में वह सब कुछ मालूम कर सकते हैं जो एक अनजान और अनपढ़ देहाती औरत पचास वर्ष में भी मालूम नहीं कर सकती। अगर वह सौ वर्ष भी लेबारेट्री में खड़ी रहे तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वे सब चीज़ें बेकार हैं। लगभग यही उपमा है उस इंसान की जिसको अल्लाह की वह्य का मार्गदर्शन प्राप्त न हो और वह इस प्रयोगशाला में खड़ा कर दिया जाए। अगर सांसारिक कैमिस्ट्री की यह लैब उसके सामने हो और अल्लाह की वह्य का मार्गदर्शन उसको उपलब्ध न हो तो वह इस कैमिस्ट्री को रोज़ तबाह किया करेगा। रोज़ बेहतर-से-बेहतर कुव्वतों को बरबाद करेगा। लेकिन अगर उसके सामने मार्गदर्शन मौजूद है तो उसकी सहायता से वह वर्षों का सफ़र मिनटों में तय कर सकता है। वह सदियों का सफ़र सेकंडों में तय कर सकता है। यह शरीअत की रहमत और बरकत है कि उसने मानव-जीवन के मौलिक सवालों का जवाब दे दिया है।
दूसरी चीज़ जो शरीअत ने बताई है वह इंसान की संवेदनाएँ एवं भावनाएँ हैं। हर इंसान के साथ कुछ संवेदनाएँ और भावनाएँ लगी होती हैं। अगर संवेदनाएँ और भावनाएँ सुदृढ़ हों तो पूरा मानव-जीवन सुदृढ़ होता है। और अगर भावनाएँ और संवेदनाएँ सुदृढ़ न हों तो पूरा जीवन कमज़ोर हो जाता है और उसके जीवन में ठहराव नहीं रहता। आपने देखा होगा कि बहुत-से लोग, जो भावुक दृष्टि से परेशानी का शिकार रहते हैं, उन्हें कभी भावनात्मक शान्ति उपलब्ध नहीं होती। उन्हें अगर दुनिया की तमाम नेमतें उपलब्ध हों तब भी उनका जीवन सफल नहीं होता। लेकिन बहुत-से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर कोई नेमत प्राप्त न भी हो, लेकिन भावनात्मक स्थिरता उपलब्ध हो तो उनका जीवन बड़ा सफल होता है। कभी-कभी बहुत छोटी-सी चीज़ इंसान की भावनात्मक स्थिरता को ख़राब कर देती है। उदाहरणार्थ कुछ लोग बड़ी ख़ुशी के माहौल में बैठे हों, अत्यन्त प्रसन्नता का अवसर हो, वहाँ मौजूद एक व्यक्ति को कोई आकर बता दे कि आपके अमुक सम्बन्धी का इंतिक़ाल हो गया है, अचानक उसकी कैफ़ियत बदल जाएगी और वह इस माहौल में नहीं रहेगा, वह शारीरिक रूप से तो वहाँ पर मौजूद रहेगा, उसकी आँखें, कान और नाक तमाम अंग काम कर रहे होंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह न सुन रहा होगा, न देख रहा होगा। एक घंटे के बाद पता चलता है कि यह ख़बर तो ग़लत थी, उसके सम्बन्धी का नहीं, बल्कि उसके किसी हमनाम का इंतिक़ाल हो गया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति दोबारा इस माहौल में वापस आ जाएगा। अब आप उससे पूछें कि अमुक ने क्या कहा था तो उसको याद नहीं रहेगा। उससे पूछें कि इस दौरान क्या हुआ था, अगर टेलीविज़न चल रहा था तो पूछ लें कि टीवी पर क्या हो रहा था, उसको पता नहीं होगा। उस्ताद लेक्चर दे रहा हो तो उसको पता नहीं होगा कि क्या कहा जा रहा था। इसलिए कि भावनात्मक रूप से वह उस वक़्त स्थिर नहीं था। यह महत्व है भावनात्मक स्थिरता का। भावनात्मक स्थिरता की प्राप्ति एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण चाहती है। यह वह नैतिक गुण और आध्यात्मिक गुण चाहती है, जो पवित्र क़ुरआन और क़ानूने-शरीअत इंसानों में पैदा करना चाहता है और पैदा करने की शिक्षा देता है। यह शरीअत का दूसरा मौलिक भाग है।
थोड़ा-सा ग़ौर करें तो अनुमान होगा कि ये दोनों हिस्से तीसरे हिस्से की तैयारी के लिए हैं। आख़िर इंसान मौलिक सवालों का जवाब क्यों चाहता है? इसलिए कि उसे जीवन गुज़ारने का ढंग बनाना है। उसे जीवन संवारने का तरीक़ा अपनाना है। इंसान भावनात्मक स्थिरता क्यों चाहता है? इसलिए कि जीवन सफलता से गुज़ारना है। मानो अस्ल जीवन गुज़ारने के लिए शरीअत ने जो मार्गदर्शन किया है, वह शरीअत का तीसरा मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीअत का वह अंग जो इंसान के व्यावहारिक जीवन को संवारता है, इंसान के ज़ाहिरी और व्यावहारिक जीवन को जो अंग संगठित करता है वह शरीअत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह वह अंग है जिसको फ़िक़्ह कहते हैं।
फ़िक़्ह की परिभाषा
फ़िक़्ह का शाब्दिक अर्थ गहरी अन्तर्दृष्टि और गहरी समझ है। किसी चीज़ की गहरी समझ को अरबी भाषा में फ़िक़्ह कहते हैं। लेकिन पारिभाषिक दृष्टि से फ़िक़्ह से मुराद है शरीअत के व्यावहारिक आदेश का वह विस्तृत ज्ञान, जो विस्तृत तर्क के आधार पर हो। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। फ़िक़्ह की परिभाषा में अरबी के शब्द हैं الفقہ ھوالعلم بالا حکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتھا التفصیلیۃ अर्थात् “फ़िक़्ह से मुराद शरीअत के उन आदेशों का ज्ञान है जो व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हों और जो शरीअत के विस्तृत तर्क से उद्धृत हूँ।
फ़िक़्ह और क़ानून के दरमियान अन्तर
अगर कोई आदेश इंसान के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखता हो, लेकिन शरीअत के विस्तृत तर्क से उद्धृत न हो तो वह फ़िक़्ह नहीं है। फ़िक़्ह वह है जो शरीअत के विस्तृत तर्क से सम्बन्ध रखता हो, उनसे उद्धृत हो और इंसान के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखता हो। उदाहरण के रूप में बहुत-से मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनका सम्बन्ध इंसान की बुद्धि से, या इंसानी संवेदनाओं से हो, वह मामले शरीअत के आदेश तो हो सकते हैं, लेकिन वे फ़िक़्ह के आदेश नहीं होंगे। इसलिए कि उनका सम्बन्ध इंसान के व्यावहारिक जीवन से नहीं होता। इसी तरह ऐसे मामले जिनका इंसान के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध हो लेकिन वे आदेश शरीअत के विस्तृत तर्क पर आधारित न हों, उनका सम्बन्ध भी फ़िक़्ह से नहीं है। उदाहरण के रूप में इंग्लिस्तान में ट्रैफ़िक के क़ानून हैं। वहाँ के ट्रैफ़िक क़ानूनों में सम्भवत: कोई भी चीज़ शरीअत से टकराती नहीं होगी। इन क़ानूनों में यही लिखा है कि अपने रुख़ पर चलो। दूसरों का हक़ न मारो। जब इधर से बत्ती लाल हो तो रुक जाओ और हरी हो तो चले जाओ। जिसका हक़ पहले आने का हो वह पहले आएगा और जिसका बाद में हो वह बाद में आएगा। ये सब क़ानून और उसूल न्याय पर आधारित हैं, और उनमें कोई चीज़ शरीअत से टकराती नहीं है, लेकिन यह फ़िक़्ह नहीं है। इसलिए कि उनमें कोई भी आदेश ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से शरीअत के विस्तृत तर्कों से उद्धृत और उनपर आधारित हो।
जो आदेश या क़ानून शरीअत के विस्तृत मूलस्रोतों से उद्धृत होगा केवल वही फ़िक़्ह कहलाएगा, और केवल ऐसे ही आदेशों के संग्रह का नाम फ़िक़्ह होगा। यों फ़िक़ही आदेशों में से हर आदेश का अटूट सम्बन्ध पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल से क़ायम है। अगर यह सम्बन्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार क़ायम है तो वह फ़िक़्ही आदेश है वरना वह सिर्फ़ क़ानून है, फ़िक़्ह नहीं है। फ़िक़्ह के हर आंशिक आदेश में शरीअत के विस्तृत तर्कों से यह सम्बन्ध पाया जाना ज़रूरी है। उदाहरण के रूप में फ़िक़्ह की कोई भी किताब उठाकर देख लें। उसमें आपको बहुत-से आदेश मिलेंगे। उदाहरणार्थ यह पानी पाक है। इससे वुज़ू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बारिश का पानी पाक है। इससे वुज़ू जायज़ है। यह एक व्यावहारिक बात है, वुज़ू करना एक व्यावहारिक चीज़ है। और पानी के बारे में मसला आपको बताया जा रहा है। यह फ़िक़्ह है। इसलिए कि इस मसले का शरीअत के विस्तृत तर्कों से सम्बन्ध है। पवित्र क़ुरआन की आयत है—“हमने आसमान से ऐसा पानी उतारा जो पाक करनेवाला है।” (क़ुरआन, 25:48) चूँकि बारिश के पानी को पवित्र क़ुरआन ने और शरीअत ने पाक कर देनेवाला क़रार दिया है अत: बारिश के पानी से वुज़ू किया जा सकता है। यह एक आदेश हुआ जिसका सम्बन्ध विस्तृत तर्कों के साथ है। यानी पवित्र क़ुरआन की सम्बन्धित आयत या सुन्नत की कोई सम्बन्धित नस (स्पष्ट आदेश); कोई हदीस हो या किसी सहाबी या ताबिई का बयान हो कि नबी (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) के ज़माने में यह तरीक़ा था। उससे जब तक सीधा सम्बन्ध नहीं होगा उस वक़्त तक उसे फ़िक़्ह नहीं कहा जाएगा। गोया फ़िक़्ह अपनी अस्ल और अपनी हक़ीक़त के अनुसार, यानी by definition शरीअत से सम्बद्ध है।
फ़िक़्ह का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि अभी कहा गया, गहरी अन्तर्दृष्टि और गहरी समझ है। आपके ज़ेहन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि इस विशुद्ध व्यावहारिक विषय का गहरी अन्तर्दृष्टि से क्या सम्बन्ध हो सकता है। क्यों गहरी अन्तर्दृष्टि उसको कहा गया। इस विषय को गहरी अन्तर्दृष्टि के नाम से क्यों याद किया गया। थोड़ा-सा ग़ौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस नाम में और इस विषय में गहरी समानता और बड़ी सूक्ष्म अनुकूलता पाई जाती है जिसका आपको ज़रा-सा ग़ौर करने से अनुमान हो जाएगा।
आप सबने पवित्र क़ुरआन पढ़ा है। क़ुरआनी आयतों की कुल संख्या छः हज़ार छः सौ से कुछ अधिक है। इसी तरह कुल हदीसें जो हदीस की तमाम किताबों में लिखी हुई हैं उनकी संख्या चालीस और पचास हज़ार के दरमियान है। चालीस और पचास हज़ार के दरमियान जो संख्या है यह इन तमाम हदीसों की है जो इस वक़्त उपलब्ध संग्रहों में मौजूद हैं। उनमें जो हदीसें आदेशों से सम्बन्धित हैं और इंसान के जीवन के व्यावहारिक आदेशों से बहस करती हैं, उनकी संख्या चार हज़ार से ज़्यादा नहीं है। पवित्र क़ुरआन की 6,666 आयतों [यह आंकड़ा केवल मुसलमानों की भावनाओं को प्रभावित करने और उन्हें चकित करने के लिए बताया जाता है, जबकि वास्तव में क़ुरआन में कुल आयतों की संख्या 6236 है——अनुवादक] में वे आयतें जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक आदेशों से है, उनकी संख्या चार-सौ से अधिक नहीं। गोया शरीअत के कुल 56 हज़ार स्पष्ट आदेशों में 4 हज़ार 4 सौ हैं जिनका सम्बन्ध व्यावहारिक आदेशों से है। शेष बावन हज़ार के क़रीब स्पष्ट आदेशों का सम्बन्ध जीवन के दूसरे पहलुओं से और मामलात से है। अब ये चार हज़ार चार-सौ स्पष्ट आदेश व्यावहारिक जीवन में इंसान को पेश आनेवाले बहुत-से मामलों से सम्बन्धित हैं, इंसान को जीवन में प्रतिदिन हज़ारों मामले उसके व्यावहारिक जीवन में पेश आते हैं। हज़ारों-लाखों, बल्कि अरबों इंसानों के जीवन में आनेवाले बहुत-से मामले हैं जो इन चार हज़ार चार-सौ स्पष्ट आदेशों के द्वारा नियमबद्ध और regulate हो रहे हैं। यह व्यावहारिक समस्याएँ क्या हैं? और उनकी क़िस्म क्या है? उनमें आपके जीवन का हर व्यावहारिक पहलू, जीवन की हर गतिविधि और जन्म से मृत्यु तक की जानेवाली हर स्वैच्छिक हरकत शामिल है। आपने रात बिस्तर पर आराम किया। बिस्तर पर सोना एक व्यावहारिक काम है। इसके बाद सुबह उठे, वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नाशता किया। ये सब व्यावहारिक काम हैं। कपड़े इस्तिरी किए, धोए, यह व्यावहारिक काम है। फिर घर के अन्य काम पूरे किए, ये सब व्यावहारिक काम हैं। अब आप यहाँ बैठे हैं, यह भी एक व्यावहारिक काम है। रात तक और अगली सुबह तक, बल्कि जीवन के आख़िरी लम्हे तक जो काम भी होगा वह फ़िक़्ह के दायरे में होगा, इसलिए कि ये सब व्यावहारिक काम हैं। इन सबका मार्गदर्शन इन चार हज़ार चार सौ स्पष्ट आदेशों में मौजूद है। जीवन का कोई विभाग ऐसा नहीं है जो इन चार हज़ार चार सौ स्पष्ट आदेशों के क्रियान्वयन से बाहर हो। मेरा और आपका यह चश्मा प्रयुक्त करना, आपका यह सफ़ेद रंग और नीले और भूरे रंग का गाउन प्रयुक्त करना, यह गिलास प्रयुक्त करना, इस पानी को पीना। ये सब बातें उन असीमित कामों में शामिल हैं जो सब इन चार हज़ार चार-सौ स्पष्ट आदेशों के कंट्रोल में हैं। इन स्पष्ट आदेशों की हैसियत उस लगाम की-सी है जिन्होंने इच्छाओं के इन असीमित घोड़ों को अपने क़ाबू में किया हुआ है। इंसानी कर्म उसकी इच्छाओं के अधीन हैं। जब तक इच्छाएँ और इरादे न हों कर्म जन्म नहीं ले सकते। इच्छाओं के इन मुँह-ज़ोर घोड़ों की लगामें इन चार हज़ार चार सौ स्पष्ट आदेशों के हाथ में हैं। इन स्पष्ट आदेशों ने इन सबको सीधे रास्ते पर रखा हुआ है। यह कितना असाधारण काम है। सच तो यह है कि आप ग़ौर करें तो दुनिया के किसी भी क़ानून में इसका उदाहरण नहीं मिलता।
दुनिया की किसी व्यवस्था में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। बेइन्तिहा इंसानों के असीमित मामलों पर इन स्पष्ट आदेशों को कैसे चस्पाँ किया जाएगा, इसके लिए बड़ी गहरी अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है। अत्यन्त गहरी सोच की आवश्यकता है। यह पूरी प्रक्रिया एक अत्यन्त गहरी समझ और सोच की अपेक्षा करती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को ‘फ़िक़्ह’ के नाम से याद किया गया। फ़िक़्ह मानो वह Process या वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप वे विस्तृत नियम और मार्गदर्शन संकलित होते हैं जो मानव-जीवन के असीमित विभागों को जोड़ते और संगठित करते हैं।
फ़िक़्ह और क़ानून
इस चर्चा और उन उदाहरणों से फ़िक़्ह की पूरी हक़ीक़त और फ़िक़्ह की परिभाषा आपके सामने आ गई होगी। और यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि फ़िक़्ह और क़ानून दोनों एक चीज़ नहीं हैं। क़ानून तो उस नियम को कहते हैं जो किसी शासक ने मुक़र्रर किया हो और अदालतें अपने मुक़द्दमों का फ़ैसला उन नियमों के अनुसार करती हों। इस सरकारी और अदालती नियम को क़ानून कहते हैं। ज़रा ग़ौर करें तो अनुमान हो जाएगा कि क़ानून की पश्चिमी धारणा का बहुत कम लोगों के जीवन से सीधा वास्ता रहता है। हममें से यहाँ डेढ़ दो सौ के क़रीब लोग बैठे हुए हैं। शायद हममें से किसी को भी जीवन में कभी किसी अदालत में जाने का मौक़ा न मिला हो और न शायद आगे भी अदालतों और कचहरियों में जाने की आवश्यकता पड़े। इससे स्पष्ट हुआ कि क़ानून का होना या न होना या अदालत में उसका स्वीकार किया जाना या न किया जाना, हमारे और आपके नित्य जीवन से इसका कोई ज़्यादा और सीधा सम्बन्ध नहीं है। आपके जीवन के मुश्किल से दो-चार प्रतिशत मामले होंगे जो देश के क़ानून के सीधे दायरे में आते होंगे। लेकिन इसके विपरीत जीवन का कोई भी काम या अमल ऐसा नहीं जो फ़िक़्ह के दायरे में न आता हो। आपकी हर व्यावहारिक और शारीरिक गतिविधि फ़िक़्ह के दायरे में आएगी। जबकि क़ानून के दायरे में आपकी नित्य गतिविधियों में से बहुत थोड़ी आएँगी। हमारी और आपकी अति महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय व्यावहारिक गतिविधियों में भी मुश्किल से एक या दो प्रतिशत ऐसी होंगी जो सीधे क़ानून से प्रभावित होंगी या उसके दायरे में आएँगी।
इससे अनुमान हो जाएगा कि फ़िक़्ह का दायरा क़ानून के दायरे से सैंकड़ों गुना बड़ा है। अगर फ़िक़्ह के दायरे में पाँच सौ चीज़ें आ रही हैं तो क़ानून के दायरे में पाँच दस चीज़ें ही आएँगी। इसलिए जिसको अंग्रेज़ी में Law कहते हैं या जिसके लिए उर्दू में क़ानून की शब्दावली प्रचलित है, वह मुश्किल ही से फ़िक़्ह के एक दो प्रतिशत मामलों को कवर करता है। शेष मामले वे हैं जिनके लिए फ़िक़्ह ही की शब्दावली प्रयुक्त की जानी चाहिए, उनके लिए क़ानून की शब्दावली प्रयुक्त करना एक सीमित चीज़ को असीमित पर चस्पाँ करने के समान है।
फ़िक़्ह का राज इंसान के जन्म से पहले शुरू हो जाता है और जन्म के बाद तक जारी रहता है। इंसान अपने जन्म से पहले ही फ़िक़्ह के कार्यक्षेत्र में आ जाता है। और मरने के बाद भी उसपर फ़िक़्ह का राज जारी रहता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक व्यक्ति का इंतिक़ाल हो गया। उसने बहुत सारे वारिस छोड़े। इंतिक़ाल के छः महीने बाद एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन यह बच्चा जो छः महीने बाद पैदा हुआ है, उसने विरासत के बँटवारे की प्रक्रिया को रोक दिया। बच्चे ने आदेश दिया कि चूँकि में आनेवाला हूँ, अत: मेरे बाप की विरासत के बँटवारे की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। और शरीअत के आदेशों और पाकिस्तान में अदालतों के आदेशों के अनुसार विरासत के बँटवारे की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। जब वह बच्चा दुनिया में आ जाएगा और वह बाप की विरासत में से अपना हिस्सा ले-लेगा तो फिर शेष वारिसों को हिस्सा मिलेगा। फिर यह बच्चा साठ सत्तर वर्ष जिया और जब दुनिया से जाने लगा तो उसने एक वक़्फ़ क़ायम कर दिया। एक बड़ी संस्था क़ायम कर दी कि नीचे मस्जिद होगी ऊपर दर्सगाहें (मदरसे) होंगी, दुकानें और मुसाफ़िर ख़ाने होंगे और ग़रीब लोग यहाँ आकर ठहरा करेंगे और पढ़ा करेंगे। वह व्यक्ति यह वक़्फ़ क़ायम करके स्वयं तो इस दुनिया से चला गया। अब अगर यह मुसाफ़िरखाना और मस्जिद और मदरसे पाँच सौ बरस भी मौजूद रहें तो उसी मरनेवाले के फ़ैसले के अनुसार इन सब का प्रबन्ध किया जाएगा। इसलिए कि शरीअत का आदेश है कि “वक़्फ़ करनेवाले की शर्त की उसी तरह पैरवी की जाएगी जिस तरह शरीअत के स्पष्ट आदेशों की पैरवी की जाती है।” अगर उसने कहा था कि यहाँ केवल अंधे बच्चों को पढ़ने की अनुमति होगी तो वहाँ कोई आँखोंवाला बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए कि वह अंधे बच्चों के लिए वक़्फ़ (समर्पित) है। अगर उसने कहा हो कि यहाँ केवल लंगड़े बच्चों को शिक्षा पाने की अनुमति होगी तो इसमें केवल लंगड़े बच्चे शिक्षा पाएँगे। ग़रज़ जो उसने कहा था उसके अनुसार इस वक़्फ़ का प्रबन्ध किया जाएगा। अब अगर यह वक़्फ़ चार-सौ वर्ष चले, पाँच सौ वर्ष चले, सात सौ वर्ष चले, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। और मरनेवाले की वसीयत के अनुसार वक़्फ़ के मामलात को चलाया जाएगा। यह मानो इस बात का उदाहरण है कि उसके इंतिक़ाल के बाद भी उसकी सम्पत्ति पर फ़िक़्ह का राज जारी है। जब तक वह सम्पत्ति मौजूद है उस समय तक यह कार्यान्वयन होता रहेगा। सारांश यह कि मानव-जीवन का कोई विभाग ऐसा नहीं है जो फ़िक़्ह के कार्यक्षेत्र और फ़िक़्ह के राज से बाहर हो।
फ़िक़्ह के महत्वपूर्ण अध्याय और विषय
फ़िक़्ह के नाम से जो संग्रह हमारे सामने मौजूद है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हिस्सा वह है जिसपर व्यक्ति अमल करेंगे। मैं निजी रूप से इसपर अमल करूँगा। आप भी निजी रूप से इसपर अमल करेंगे। मैं अपने और अपने परिवारवालों की हद तक इसपर अमल करने का ज़िम्मेदार हूँ और आप अपने और अपने परिजनों की हद तक इसपर अमल करने के ज़िम्मेदार हैं। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में फ़िक़्ह का उसूल है “मुसलमान जहाँ भी हो वह इस्लाम के आदेशों का पाबंद है।” इस हिस्से में चार चीज़ें शामिल हैं। इबादतें, यानी नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज, और उनसे सम्बन्धित आदेश। पारिवारिक क़ानून यानी निकाह, तलाक़, विरासत और वसीयत के आदेश। मामलात यानी निजी क्रय-विक्रय, लेन-देन व्यक्तियों के दरमियान व्यापार, तिजारत। और चौथी चीज़ सामाजिक मामले यानी लोगों के साथ मेल-जोल सम्बन्ध, लिबास, ख़ुराक, खाना-पीना। ये चार चीज़ें वे हैं जिनमें शरीअत और फ़िक़्ह के आदेशों का हर मुसलमान हर समय और हर जगह पाबंद है। और हर हाल में पाबंद है। अगर कल मंगल ग्रह पर जीवन खोज लिया जाए और आपको मंगल ग्रह पर जाने और बसने का मौक़ा मिले तो मंगल पर भी आपको नमाज़ें अदा करनी होंगी, रोज़े रखने होंगे और ज़कात अदा करनी होगी। वहाँ से भी हज करने के लिए ज़मीन पर आना पड़ेगा। इसके आदेश क्या होंगे, मैं नहीं जानता। वहाँ नमाज़ों के वक़्तों का निर्धारण कैसे होगा, वह बाद की बात है, लेकिन नमाज़ के समयों का वहाँ के फुक़हा के इजतिहाद (रायों) के अनुसार जो भी निर्धारण होगा उसके अनुसार अमल करना होगा। वहाँ भी शराब पीना और चोरी करना जायज़ नहीं होगा, वहाँ भी मामलात शरीअत के अनुसार होंगे। निकाह और तलाक के मामले वहाँ भी शरीअत के अनुसार होंगे। वहाँ भी निकाह और तलाक़, विरासत और वसीयत के आदेशों का उल्लंघन जायज़ नहीं होगा। शराब वहाँ भी हराम रहेगी। हिजाब के आदेश वहाँ भी वही होंगे जो यहाँ हैं। पर्दा और हिजाब वहाँ भी होगा। ये चार वे चीज़ें हैं जो हर जगह, हर समय, हर हाल में मुसलमानों के लिए अनिवार्य हैं कि वे इनका पालन करें। हर मुसलमान निजी और व्यक्तिगत रूप से इन आदेशों पर अमल करने का शरीअत के अनुसार पाबंद है।
दूसरा हिस्सा फ़िक़्ह के आदेशों का वह है जिनपर अमल करना व्यक्तियों की निजी और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी नहीं। यह वे काम हैं जो सरकार या राज्य के करने के हैं। अगर मुसलमानों का राज्य होगा तो वह इन आदेशों पर अमल करेगा। और अगर मुसलमानों का राज्य नहीं होगा तो फिर व्यक्ति इन आदेशों को अपने हाथ में नहीं लेंगे।
उदाहरण के रूप में शरीअत ने फ़ौजदारी आदेश दिए हैं। चोर का हाथ काटने और क़ातिल से क़िसास (ख़ून का बदला) लेने का आदेश शरीअत ने दिया है। शरीअत ने शराबनोशी के लिए कोड़ों की सज़ा मुक़र्रर की है। व्यक्तियों को यह अनुमति नहीं कि इन आदेशों पर ख़ुद से अमल शुरू कर दें। शरीअत में इस बात की अनुमति नहीं कि किसी ने देखा कि चोरी हो गई और उसने गंडासा लिया और चोर का हाथ काट दिया। यह मेरा और आपका काम नहीं है। यह सरकार, राज्य और उसकी संस्थाओं का काम है। इसके लिए लोग सक्षम नहीं हैं। अगर आप ख़ुदा-न-ख़ास्ता इसराईल में या किसी भी ऐसे ग़ैर-मुस्लिम देश में रहते हों जहाँ मुसलमानों की सरकार न हो और वहाँ चोरी हो तो आपसे क़ियामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि अमेरिका में अमुक व्यक्ति ने चोरी की थी तुमने उसका हाथ क्यों नहीं काटा। इसलिए कि शरीअत ने यह ज़िम्मेदारी आपपर नहीं डाली। शरीअत ने शासकों से कहा है कि वे इन आदेशों पर क्रियान्वयन को निश्चित बनाएँ, अत: सरकारों और सत्ताधारियों को यह काम करने चाहिएँ। ये भी चार चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इस्लाम का दस्तूरी क़ानून है जिसपर आगे चलकर चर्चा होगी। दूसरी चीज़ इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून है। तीसरी चीज़ इस्लाम का ज़ाबिता क़ानून यानी Procedural Law है। चौथी चीज़ इस्लाम का अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून है। इन सबपर आगे चलकर बात की जाएगी कि इस्लामी राज्य के दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध या मुसलमानों के सम्बन्ध दूसरे धर्मों से कैसे हों। यह इस्लाम के अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के विषय हैं।
ये वे चीज़ें हैं जो फ़िक़्ह के तमाम विषयों को समेट लेती हैं। ये आठ मौलिक अध्याय या विषय हैं जो फ़िक़्हे-इस्लामी के अधिकतर हिस्से को समेटे हैं। इसके अलावा भी आंशिक रूप से एक दो चीज़ें और हैं। लेकिन बड़े-बड़े अध्याय यही हैं।
इन अध्यायों और विषयों को समझने की ख़ातिर विभिन्न लोगों ने विभिन्न शीर्षकों के तहत बयान किया है। कुछ ने कहा कि शरीअत के आदेशों में मौलिक चीज़ें दो हैं; आदाब और इबादात। कुछ ने कहा कि शरीअत में इबादात और मामलात दो बड़े-बड़े अंग हैं। कुछ ने कहा इबादात, आदाब और मामलात तीन चीज़ें हैं। लेकिन ये सारे विभाजन समझने के लिए और छात्रों की आसानी की ख़ातिर हैं। जो अबवाब हैं वे सब किताबों में एक जैसे हैं। चुनाँचे फ़िक़्ह की अधिकतर किताबों में आरम्भ ‘तहारत’ और ‘पाकीज़गी’ के मसाइल से होता है। इसलिए कि इंसान को सबसे पहले जिन आदेशों की आवश्यकता पड़ती है वे यही समस्याएँ हैं। अगर आज उस वक़्त पौने तीन बजे कोई व्यक्ति मुसलमान हो जाए, तो सबसे पहले शरीअत के जिस आदेश का पालन करना पड़ेगा वह ज़ुह्र की नमाज़ है। उससे कहा जाएगा कि अभी ज़ुह्र की नमाज़ का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ। आप समझदार और वयस्क हैं, अब आप चूँकि मुसलमान हो गए हैं इसलिए आपपर नमाज़ फ़र्ज़ है, अत: तुरन्त ज़ुह्र की नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के लिए पहली बात उससे यह कही जाएगी कि जाकर ग़ुस्ल (स्नान) करो। ग़ुस्ल करने के लिए उसको यह भी बताना होगा कि पाक पानी कौन-सा है और नापाक कौन-सा है। उसको यह बताना पड़ेगा कि पाकी क्या है और नापाकी क्या है। इसलिए सबसे पहले जो व्यावहारिक मसला एक मुसलमान के सामने आएगा वह पाकी और नापाकी का होगा। उसके बाद नमाज़ के आदेश और समस्याओं (मसाइल) से उसका सामना होगा। कुछ महीनों के बाद रमज़ान आ गया तो उसे रोज़े रखने होंगे। सम्भव है वह बूढ़ा हो, कमज़ोर हो या बच्चा हो और रोज़े न रख सकता हो। इसलिए सम्भव है उसको रोज़े रखने की आवश्यकता न पड़े। वर्ष भर के बाद ज़कात का मसला आएगा तो ज़कात के आदेश आएँगे। गोया सबसे पहले उसको इबादतों से वास्ता पड़ेगा। फिर व्यक्तिगत क़ानूनों से वास्ता पड़ेगा। ज़ाहिर है वह एक ख़ानदान का सदस्य होगा। सम्भव है कि पहले से उसके बीवी बच्चे भी हों, उसके माँ-बाप हों, बहन-भाई हों। उनसे कैसे मामला करेगा। उनसे सम्बन्धों को कैसे संगठित करे। इन मामलों के लिए व्यक्तिगत क़ानूनों की आवश्यकता पेश आएगी। फिर उसको बाज़ार में जाकर क्रय-विक्रय करना होगा। उसके लिए मामलों के आदेश दरकार होंगे। फिर उसको यह बताना होगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है, पर्दे के आदाब (शिष्टाचार) क्या हैं, पुरुषों और महिलाओं के दरमियान मेल-जोल के शिष्टाचार एवं नियम और सीमाएँ क्या हैं। ये सब मामलात उसको बताने होंगे और वह उनका पालन करेगा। फ़िक़्ह की किताबों में इसी क्रम के साथ आदेश लिखे हुए हैं। और मुसलमानों को जिन आदेशों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वे पहले हैं और जिनकी कम आवश्यकता पड़ती हैं वे बाद में हैं। यह वह संग्रह है जिसको फ़िक़्ह कहते हैं।
इस चर्चा से आपने यह अनुमान कर लिया होगा कि अपनी व्यापकता और सारगर्भिता में यह संग्रह दुनिया के तमाम क़ानूनों से बढ़कर है। दुनिया के तमाम क़ानून या तो उन मामलों से बहस करते हैं जिनमें दो इंसानों के दरमियान कोई व्यापारिक मेल-जोल या कोई कारोबारी लेन-देन का सम्बन्ध होता हो, या वहाँ सरोकार रखते हैं जहाँ किसी इंसान ने कोई ग़लती की हो या उससे कोई अपराध हो गया हो। इन दो के अलावा अधिकतर क़ानूनों ने दूसरे महत्वपूर्ण विषयों का नोटिस नहीं लिया। दुनिया के क़ानूनों को इससे कोई ग़रज़ और दिलचस्पी नहीं होती कि मानव-जीवन इस सीमित परिधि के अलावा भी होती है। जहाँ दो व्यक्तियों के दरमियान लेन-देन है उसको संगठित करने के लिए क़ानून आगे आता है, या जहाँ किसी इंसान से ग़लती या अपराध हो जाए उसकी सज़ा देने के लिए क़ानून हरकत में आता है। इन दो बातों के अलावा दुनिया के क़ानूनों को आम तौर पर दिलचस्पी ही नहीं होती कि मानव-जीवन में और क्या-क्या हो रहा है। जबकि फ़िक़्हे-इस्लामी की दिलचपसी रात को बिस्तर पर सोने से लेकर और अगली रात सोने तक और जब तक यह जीवन है उसके अन्तिम क्षण तक हर इंसानी गतिविधि से है। उसके बाद भी फ़िक़्ह हमें बताती है कि मरनेवाले को मरने के बाद रुख़स्त कैसे किया जाए। यानी स्वागत करने से लेकर विदा करने तक के तमाम चरणों और एक-एक चीज़ के बारे में निर्देश और मार्गदर्शन मौजूद है। यह संग्रह अपनी व्यापकता और सारगर्भिता की दृष्टि से दुनिया के तमाम संग्रहों से अलग और नुमायाँ है।
फ़िक़्ह का कार्यक्षेत्र
फिर दुनिया के क़ानून एक दृष्टि से दो हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ क़ानून वे हैं जो धार्मिक क़ानून कहलाते हैं और कुछ क़ानून वे हैं जो सांसारिक क़ानून कहलाते हैं। इन दोनों का कार्यक्षेत्र दुनिया में हर जगह अलग-अलग है। पण्डित, पुरोहित, पादरी, ये धार्मिक क़ानूनों से बहस करते हैं। अदालतें, वकील, क़ाज़ी, ये सांसारिक क़ानूनों से बहस करते हैं। इस्लाम में ये दोनों क़ानून मिले-जुले हैं। जिन किताबों में दुनिया के क़ानून लिखे हुए हैं उन्ही में दीन के क़ानून भी लिखे हुए हैं। जिन किताबों में यह लिखा है कि रात को तहज्जुद की नमाज़ कैसे अदा की जाए, उन्हीं किताबों में यह भी लिखा है कि आप विदेश मंत्री के तौर पर दूसरे देशों से व्यापारिक अनुबन्ध करें तो कैसे करें। अगर आप सेना के प्रमुख हैं और मैदाने-जंग का नेतृत्व कर रहे हैं तो यह भी इन किताबों में लिखा हुआ है कि सेनाओं का नेतृत्व कैसे करें। जिस पवित्र क़ुरआन से यह मार्गदर्शन मिला है कि आपका पड़ोसियों के साथ क्या सम्बन्ध होना चाहिए उस पवित्र क़ुरआन में यह मार्गदर्शन भी मिलता है कि समाज से अपराधों का उन्मूलन कैसे किया जाए, चोर को सज़ा कैसे दी जाए, क़ातिल को सज़ा कैसे दी जाए। यानी इस्लामी व्यवस्था या इस्लामी फ़िक़्ह में इस आधार पर कोई भेद नहीं है कि मामले का सम्बन्ध विशुद्ध धार्मिक या आध्यामिकता के दायरे से है या उसका सम्बन्ध विशुद्ध संसार और भौतिकवाद के दायरे से है। इन दोनों दायरों के मामलों से एक ही किताब में एक ही जगह बहस हो रही है और इन दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। यह द्वंद्व जब इंसानी समाज में पैदा हो जाता है तो वह समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब इंसानी समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है तो मानव व्यक्तित्व दो भागों में विभाजित हो जाता है। फिर मानव-जीवन में एकता का पैदा करना सम्भव नहीं रहता। यह बात दुनिया के प्राचीन धर्मों ने या तो समझी नहीं, और अगर समझी तो बाद में आनेवालों ने इसको भुला दिया। इस भुलावे के परिणामस्वरूप उनका धर्म, उनकी सभ्यता एवं संस्कृति और उनके समाज सब दो-दो, तीन-तीन और चार-चार भागों में विभाजित हो गए और कभी इससे ज़्यादा भागों में विभाजित हो गए। और यह विभाजन-दर-विभाजन की प्रक्रिया फैलती चली जा रही है।
जब तक मुसलमान एकता की परिकल्पना पर कार्यरत रहे, رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई एक ही नमाज़ में, जो ख़ालिस दीनी और आध्यात्मिक मामला है, दोनों चीज़ों की तलब करते रहे। लेकिन इस ख़ालिस धार्मिक दुआ में भी दुनिया की बेहतरी का सवाल पहले है और आख़िरत की बेहतरी का सवाल बाद में है। इसलिए कि दुनिया पहले है और आख़िरत बाद में है। यों पवित्र क़ुरआन और शरीअत ने इन दोनों को एक कर दिया, और फ़िक़्हे-इस्लामी में ये दोनों चीज़ें इस तरह इकट्ठी हो गई हैं कि इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता।
‘इल्मे-फ़िक़्ह’ का आरम्भ और विकास
इस्लाम के आरम्भ में जब इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) फ़िक़्ह के क़ानूनों और आदेशों को संकलित कर रहे थे उस वक़्त तो यह स्थिति थी कि जब कोई नया मसला पेश आता था तो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) उसका जवाब दे दिया करते थे। उदाहरणार्थ हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) सहाबी के पास पवित्र क़ुरआन का ज्ञान भी था और सुन्नत का ज्ञान भी था। जब किसी व्यक्ति को कोई मसला पेश आता था, वह जाकर हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पूछ लिया करता था। यों पूछनेवाले पूछते थे और वह बता देते थे। इस तरह एक-एक करके हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इजतिहादात (रायें) जमा होते गए। इसी तरह हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास लोग जाया करते थे और मार्गदर्शन लिया करते थे। यों एक-एक करके उनके इजतिहादात जमा हो गए। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अबदुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा), हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु), ज़ैद-बिन-साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) वग़ैरा जैसे बड़े-बड़े सहाबा के इजतिहादात एक-एक करके जमा होते गए। और ताबिईन (वे ईमानवाले व्यक्ति जिन्हें सहाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ) उनको संकलित करते गए। फिर ताबिईन के इजतिहादात बाद में आनेवाले लोगों के पास पहुँचते गए, जमा होते गए और क्रमशः किताबी शक्ल में संकलित होते रहे।
पहली सदी हिजरी में यह सारा काम मुकम्मल हो गया। सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने पवित्र क़ुरआन को जितना समझा और उससे जो आदेश निकाले, वह उन्होंने ताबिईन तक मुंतक़िल कर दिए। ताबिईन ने जितना समझा और जो आदेश संकलित किए वे उन्होंने तबा-ताबिईन (वे लोग जिन्हें सहाबा का दीदार करनेवालों यानी ताबिईन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ) तक स्थानांतरित कर दिए। तबा-ताबिईन ने ये सारे इजतिहादात अपने शागिर्दों तक स्थानान्तरित कर दिए। जब ताबिईन और तबा-ताबिईन के शागिर्दों का ज़माना आया, तो उन्होंने अलग-अलग किताबें संकलित करनी शुरू कीं। यानी पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर (टीका) और हदीस के मजमुओं से अलग कुछ किताबें जिनमें विस्तृत इजतिहादात और फ़िक़ही आदेश लिखे गए थे। उनमें सबसे पहली किताब किसने लिखी? यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जो किताबें पाई जाती हैं उनमें प्राचीनतम किताब किताब ‘अल-मजमूअ’ है जो इमाम ज़ैद-बिन-अली ने लिखी थी जो हज़रत इमाम हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पोते और हज़रत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के साहबज़ादे थे। यह अली जिनके सम्बन्ध से इमाम ज़ैद को ज़ैद-बिन-अली कहा जाता है, वे हैं जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहलाते हैं। वंशावली यों है— इमाम ज़ैद-बिन-अली-बिन-इमाम ज़ैनुल-आबिदीन-बिन-हुसैन-बिन-अली-बिन-अबी-तालिब। फ़िक़्ह की सबसे पहली किताब इन्हीं ज़ैद-बिन-अली ने लिखी थी, उन व्यावहारिक आदेशों पर जिनको आज फ़िक़्ह कहते हैं। यह किताब पहली सदी हिजरी के अन्त और दूसरी सदी हिजरी के आरम्भ में लिखी गई। आज हमारे पास इससे पहले लिखी गई फ़िक़्ह की कोई विधिवत किताब मौजूद नहीं है।
इसके बाद दूसरी किताबें जो हम तक पहुँची हैं, वे इमाम अबू-हनीफ़ा के शागिर्दों और उनके समकालीन फ़ुक़हा की किताबें हैं। इमाम मालिक (रह॰), इमाम औज़ाई (रह॰), इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰)। इनका विस्तृत उल्लेख मैं बाद में करूँगा। लेकिन जब दूसरी सदी हिजरी का आरम्भ हुआ और मुस्लिम जगत् की सीमाएँ दिन-प्रतिदिन फैलती चली गईं तो प्रतिदिन ऐसे मसाइल (समस्याएँ) पेश आते थे जिनके जवाब शरीअत की रौशनी में दरकार थे। आए दिन हर बड़े-छोटे शहर और बस्ती में नए मार्गदर्शन की आवश्यकता पेश आती रहती थी। इन परिस्थितियों में इस बात का ख़तरा मौजूद था कि किसी विश्वसनीय और प्रमाणित फ़क़ीह के न होने से लोग कम जानकारी से ग़लत फ़ैसले न कर दें। या किसी कम जानकारीवाले आदमी से जाकर पूछने लगें और कोई ग़लत राय क़ायम कर लें। उस ज़माने में मुस्लिम जगत् की सीमाएँ चीन से लेकर स्पेन तक फैली हुई थीं। स्पेन और फ़्रांस की सीमा के दरमियान ‘ले पेरिने’ नाम का एक पहाड़ी सिलसिला आता है। इसकी सीमाओं से लेकर पूरा स्पेन, आधा पुर्तगाल, पूरा उत्तरी अफ़्रीक़ा, पूरा मध्य-पूर्व, पूरा अफ़ग़ानिस्तान, पूर मध्य एशिया, पूरा ईरान और चीन की उत्तरी सीमा तक मुस्लिम जगत् की सीमाएँ थीं। अब यहाँ इस बात की सम्भावना हर समय मौजूद थी कि किसी गाँव में, किसी देहात में, किसी सीमावर्ती इलाक़े में, नव-मुस्लिमों की किसी बस्ती में, किसी आदमी को कोई मसला पेश आए और वहाँ जवाब देनेवाला कोई परिपक्व ज्ञानी और परिपक्व फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) उपलब्ध न हो, या मौजूद हो लेकिन कच्चा फ़क़ीह हो। या कच्चा भी न हो, लेकिन उस मामले में उसके पास निर्देश मौजूद न हो। हो सकता है कि ग़लत जवाब दे दे। यों लोग अल्लाह और उसके रसूल की शरीअत को ग़लत समझ लें और ग़लत तरीक़े से अमल करें। इन परिस्थितियों में कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह महसूस किया कि इस बात की आवश्यकता है कि नई-नई समस्याओं का सोच-सोचकर जवाब दिया जाए। बजाय इसके कि हम इंतिज़ार में बैठें कि कोई आकर वस्तुस्थिति और सम्भावित समस्या बयान करके शरीअत का मसला पूछे तो हम जवाब देंगे। हमें ख़ुद से ग़ौर करके सम्भावित सवाल और सम्भावित मामले फ़र्ज़ करने चाहिएँ और उनका जवाब तैयार करके रखना चाहिए।
यह फ़िक़्ह का वह हिस्सा है जिसको फ़िक़्हे-तक़दीरी कहते हैं। सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन आम तौर पर इसको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि बिना इसके कि मामला सचमुच पेश आए, ख़ुद से सोच-सोचकर सम्भावित परिस्थितियाँ मान ली जाएँ और उनका पेशगी जवाब दे दिया जाए। इसलिए सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और अधिकतर ताबिईन ने इस काम को नहीं किया। लेकिन बाद में जब आवश्यकता महसूस की गई तो तबा-ताबिईन और उनके शागिर्दों के ज़माने में यह प्रक्रिया शुरू हुई। जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत-से लोगों ने अपनी जीवनियाँ इस काम के लिए समर्पित कर दीं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰), इमाम शाफ़िई (रह॰), इमाम मालिक (रह॰), इमाम इब्ने-जरीर तबरी (रह॰), इमाम औज़ाई (रह॰), सुफ़ियान सौरी (रह॰) और इस तरह के दर्जनों लोग थे जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और अपनी जीवनियाँ लगाकर इस महान काम को पूरा किया। ये लोग मामलात पर ग़ौर कर-करके और उनके आदेश तलाश कर-करके किताबें संकलित करते गए। इस चीज़ को फ़िक़्हे-तक़दीरी कहते थे। कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने कमो-बेश 84 हज़ार मसाइल (समस्याओं) का जवाब सोचा और संकलित कराया। उनके शागिर्दों ने इमाम साहिब के सिद्धान्तों से काम लेकर लगभग पाँच लाख और मसाइल का जवाब सोचा और संकलित कराया। उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने और पाँच लाख मसाइल का जवाब सोचा और संकलित किया। इस तरह केवल इमाम अबू-हनीफ़ा और उनके शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों ने दस लाख 84 हज़ार मसाइल का पेशगी अनुमान किया, उनपर सोचा और उनका जवाब संकलित किया। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने आठ जिल्दों का एक इंसाइक्लोपेडिया लिखा, जिसका एक भाग इतना मोटा है कि उसमें हज़ारों समस्याओं से बहस की गई है। इन सब भागों में जितने मसाइल बयान हुए हैं मुझे उनकी सही संख्या तो मालूम नहीं लेकिन इतना मालूम है कि यह संख्या लाखों में ज़रूर है। जीवन की किसी भी समस्या के बारे में जो जवाब क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में इमाम शाफ़िई के ज़ेहन में आया, वे सोचते गए और जवाब देते गए। उनका तरीक़ा यह था कि पवित्र क़ुरआन की एक-एक आयत लेते थे, उसपर ग़ौर करते थे, अपने शागिर्दों से विचार-विमर्श करते थे और जो-जो मसाइल (विस्तृत आदेश) उनसे निकलते जाते थे वे लिखते जाते थे। फिर हदीसों को लेते थे। एक-एक हदीस से जो मसाइल निकलते रहते थे वे उन्हें लिखते रहते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत-सी किताबें लिखीं जो एक बड़ी किताब के रूप में जमा हैं जिसको ‘किताबुल-उम्म’ कहते हैं।
यह सिलसिला दूसरी सदी हिजरी से शुरू हुआ और कई सदियों तक जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा फ़िक़ही संग्रह संकलित हुआ जो दुनिया के पूरे इतिहास में अद्वितीय है। न केवल मानव-ज्ञान के इतिहास में, बल्कि मुसलमानों के इतिहास में भी इसके उदाहरण किसी और ज्ञानपरक प्रयास में नहीं मिलते। यह मुसलमानों के सामूहिक चिन्तन का परिणाम है। इसमें लाखों बेहतरीन दिमाग़ों ने भाग लिया है। इसमें लाखों इंसानों के लाखों दिन और लाखों रातें बीती हैं। इसके परिणामस्वरूप आज ये किताबें, जिनसे पुस्तकालय भरे हुए हैं, संकलित रूप में हमारे सामने हैं।
फ़िक़्हे-इस्लामी के क्रमबद्ध करने और संकलन का यह अद्वितीय कार्य किसी अन्तरिक्ष में नहीं हुआ। यह सारा काम नित्य के तथ्यों की रौशनी में हुआ। नित्य की सांस्कृतिक आवश्यकताओं और सरकार की समस्याओं को सामने रखकर किया गया। इस सारे संग्रह में मुसलमानों की तमाम-तर सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इसलिए उसका सम्बन्ध मानव-जीवन के हर विभाग से है। मानव-जीवन के नित्य मामलों से लेकर इस्लामी सभ्यता और समाज के तथ्यों, इस्लामी संस्कृति में प्रतिदिन पेश आनेवाली समस्याएँ और मामले सबसे इस विस्तृत मार्गदर्शक ग्रन्थ का गहरा सम्बन्ध है। इसलिए उसकी हैसियत एक पल के लिए भी मात्र किसी वैचारिक मत या निराली राय की नहीं थी, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शक-पत्र था जो लाखों इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों), करोड़ों इंसानों को रात-दिन उपलब्ध कर रहे थे। उसका आधार पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में है। उसका सम्बन्ध नैतिक आचरण से अत्यन्त गहरा है। दुनिया के सेक्युलर क़ानूनों की तरह यह कोई अनैतिक या नैतिकता रहित व्यवस्था नहीं है। नैतिक आचरण के बारे में यह व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है। बल्कि जैसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, यह इस्लाम की नैतिक शिक्षाओं और निर्देशों से गहरे तौर पर सम्बद्ध है। हर फ़िक़ही आदेश के सीधे नैतिक तथा आध्यात्मिक परिणाम बयान किए गए हैं। पवित्र क़ुरआन की सैंकड़ों आयतें ऐसी हैं जहाँ फ़िक़ही आदेश बताए गए हैं, और वहीं इन आदेशों के नैतिक और आध्यात्मिक परिणामों की निशानदेही भी की गई है। “ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ” इस आदेश पर अमल करने से तुम्हारे अन्दर तक़्वा (ईशपरायणता) पैदा होगा। “ताकि तुम याददिहानी हासिल करो” इस निर्देश को मानने से तुम अल्लाह को याद रखोगे, “और क़िसास में तुम्हारे लिए जीवन है” और “इस तरह मालो-दौलत तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान गर्दिश नहीं करेगी।” गोया हर क़ानून के साथ उसके फल, नैतिक परिणामों और आध्यात्मिक बरकतों की निशानदेही की गई है। इस तरह इस्लाम में फ़िक़ही आदेश, क़ानून, धार्मिक मार्गदर्शन, नैतिक बरकतें, आध्यात्मिक फल ये सारी चीज़ें आपस में पूरी तरह सम्बद्ध हैं, और उनको एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें मानव स्वभाव और मनोविज्ञान का इस तरह ध्यान रखा गया है कि कोई आदेश और कोई नियम मानव मनोविज्ञान, मानव स्वभाव और मानव प्रतिष्ठा से टकराता नहीं है।
रात में एक किताब पढ़ रहा था। अल्लामा महमूद-बिन-अहमद बदरुद्दीन ऐनी का नाम आपने सुना होगा। यह बड़े फ़क़ीह थे और उन्होंने सहीह बुख़ारी की एक शरह (व्याख्या) भी लिखी है। उनकी एक किताब है ‘अल-बिनाया’, यह ‘हिदाया’ की शरह है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सफ़र पर जा रहा हो और उसके पास पानी न हो, लेकिन हमराही के पास पानी मौजूद हो, तो क्या उसकी यह शरई ज़िम्मेदारी है कि वह हमराही से पानी माँगे और वुज़ू करे? या वह ‘तयम्मुम’ (मिट्टी पर हाथ मारकर मुँह और हाथों पर फेरना) करके काम चला सकता है। इसपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बहस की है और यह पूरी बहस इस किताब के दस बारह पृष्ठों पर फैली हुई है। कुछ फुक़हा का कहना है कि शरीअत ने हाथ फैलाने से मना किया है। शरीअत ने इनसान को आत्मसम्मान का आदेश दिया है और इंसानी इज़्ज़त को बरक़रार रखा है। हाथ फैलाने से प्रतिष्ठा पर अन्तर पड़ता है और इज़्ज़त को बट्टा लगता है। इसलिए शरीअत ने किसी भी काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने का पाबंद नहीं किया। अत: शरीअत में इसकी अनुमति होनी चाहिए कि वह व्यक्ति तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और अपने हमराही के सामने पानी के लिए हाथ न फैलाए।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि अगर उस व्यक्ति के पास पैसे हैं और दूसरा व्यक्ति पानी रूपयों के बदले देने के लिए तैयार है तो किस क़ीमत पर पानी लिया जा सकता है। इस तरह की समस्याओं से पता चलता है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने मानव स्वभाव और भावनाओं का कितना अधिक ध्यान रखा है। इंसान दूसरे से कोई चीज़ माँगने में संकोच करता है। कितनी भी बेतकल्लुफ़ी हो, लेकिन मुझे प्यास लगी हो और आपके पास पानी हो तो शायद मैं माँगने में संकोच करूँ। इसलिए शरीअत ने इंसान को ऐसी चीज़ का पाबन्द नहीं किया है जिसको उसकी तबीअत न मानती हो। यह इंसानी स्वभाव और मनोविज्ञान का ध्यान रखने की बात है। इसके और उदाहरण आगे चर्चा में मैं बयान करूँगा।
ये वे कुछ मौलिक विशेषताएँ हैं जो फ़िक़्हे-इस्लामी में पाई जाती हैं। फ़िक़्हे-इस्लामी अपनी व्यापकता, नवीनता, प्रकार और विशेषताओं की दृष्टि से न केवल पूरे मानव इतिहास, बल्कि इस्लामी ज्ञान-विज्ञान के इतिहास में एक निराला स्थान रखता है और उसे निस्सन्देह इस्लाम के गुलदस्ते का सबसे नुमायाँ फूल कहा जा सकता है।
सवालात
सवाल : फ़िक़्हे-तक़दीरी क्या मतभेद का कारण न बना? उनके सोचने के ढंग में अन्तर हो सकता है।
जवाब : फ़िक़ही मामलात में मतभेद बुरी चीज़ नहीं है। मतभेद अच्छी चीज़ है, अगर वह शरीअत की सीमाओं के अंदर हो। और हर व्यक्ति यह समझता हो कि यह मेरी समझ है जिसमें ग़लती की सम्भावना हो सकती है। और यह दूसरे फ़क़ीह की समझ है जिसमें सही होने की सम्भावना है। जब तक यह बात हो तो मतभेद में कोई बुराई नहीं। स्वतंत्र रूप से और निष्ठापूर्ण मतभेद से दीन की समझ बढ़ती है। सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी बहुत-से मामलात में एक से अधिक रायें मौजूद थीं। जिसके उदाहरण आपके सामने हैं। अगर इन विभिन्न रायों को दीन बना लिया जाए या शरीअत के बराबर समझा जाए तो इससे ख़राबी पैदा होती है। एक फ़क़ीह की समझ अत्यन्त सम्मान योग्य है। लेकिन इससे मतभेद भी किया जा सकता है। इसलिए कि इसमें ग़लती की सम्भावना मौजूद हो सकती है। जो चीज़ ग़लती से मुक्त है, जो सौ प्रतिशत सही है वह सिर्फ़ अल्लाह का कलाम और उसके रसूल के कथन हैं। इसके अलावा हर इंसान की समझ में, हर इंसान की अन्तर्दृष्टि में और हर इंसान के इजतिहाद में ग़लती की सम्भावना मौजूद है। यही वजह है अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अगर मुज्तहिद सही नतीजे पर पहुँचता है तो उसको दो अज्र (इनाम) मिलेंगे। और अगर ग़लती करेगा तो उसको एक अज्र मिलेगा। इसका मतलब यह है कि निष्ठापूर्ण ग़लती भी अल्लाह की नज़र में पसंदीदा है। मुज्तहिद की ग़लती अल्लाह की नज़र में ऐसी है कि जैसे आपका एक छोटा प्यारा बचा हो, जिसने अभी चलना सीखा हो। जब वह गिरता है तो आपको उसपर बहुत प्यार आता है और आप एक दम उसको गोद में उठा लेती हैं। तो गोया इंसान एक बच्चे की तरह है। वह अपने सीमित ज्ञान और बुद्धि से अल्लाह का आदेश मालूम करने की कोशिश करता है। और इसमें निष्ठा से ग़लती करता है तो वह ग़लती भी अल्लाह को प्रिय है।
सवाल : आपने अन्तिम उदाहरण में जो बताया है तो उसके अनुसार फ़िक़्ह अस्पष्ट और उलझी हुई चीज़ है?
जवाब : नहीं, फ़िक़्ह अस्पष्ट चीज़ नहीं, न ही वह उलझी हुई चीज़ है और न वह कोई अप्रिय चीज़ है, बल्कि वह इंसानों की ज़रूरितों को पूरा करनेवाली एक अपरिहार्य चीज़ है। शरीअत पर जब भी व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वयन होगा उसके विस्तृत आदेश संकलित करने पड़ेंगे। इन आदेशों को संकलित करने के लिए शरीअत के स्पष्ट आदेशों को समझना होगा, उनकी व्याख्या करनी होगी। इसी को फ़िक़्ह कहते हैं। फ़िक़्ह वक़्त के साथ-साथ बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। आपको नए-नए मामलात आए दिन पेश आते रहेंगे, और अनंत नए मामलों में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर पहले दिन से यह इरादा हो कि शरीअत पर अमल करना है। अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मंशा को जीवन में ढालना है तो फिर इंसान ख़ुद-ब-ख़ुद उसके अनुसार जीवन को ढालता चला जाता है, लेकिन अगर पहले दिन से संकल्प यह हो कि शरीअत की हर चीज़ में कीड़े निकालने हैं और मुश्किलों की निशानदेही करनी है तो आसान-से-आसान चीज़ में भी मुश्किलों की निशानदेही की जा सकती है।
दुनिया यह नहीं देखती कि उसके अपने यहाँ मुश्किलों कितनी हैं। आज से कई वर्ष पहले मैंने आठ-नौ सौ पृष्ठों की एक मोटी किताब देखी। उसमें अंग्रेज़ी प्रोटोकोल के आदाब (शिष्टाचार) लिखे हुए थे। उसमें एक पूरा अध्याय इस बारे में था कि जब किसी मेहमान को खाने की मेज़ पर बिठाओ, तो उसके आदाब क्या हैं, बर्तन कैसे रखेंगे और मेहमान को कैसे बिठाएँगे। हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे। वह पश्चिम की हर चीज़ के बड़े समर्थक थे और मुसलमानों की हर चीज़ के कड़े आलोचक थे। वे यह कहा करते थे कि मुसलमानों ने फ़िक़्ह के नाम पर दीन और जीवन दोनों को पेचीदा कर दिया है। मैंने कहा कि मुसलमानों ने जीवन को पेचीदा किया है या नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने तो ज़रूर जीवन को अत्यन्त जटिल कर लिया है। मुसलमान ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं। अंग्रेज़ों ने केवल खाना खाने पर सौ पृष्ठ लिखे हैं कि खाना कैसे खाया जाएगा। चूँकि वहाँ की बातों पर आपत्ति नहीं होती इसलिए वहाँ की हर छोटी-से-छोटी चीज़ अच्छी मालूम होती है। शरीअत के मामले में चूँकि संकोच होता है इसलिए यहाँ की हल्की और आसान चीज़ भी पेचीदा मालूम होती है। फ़िक़्ह की कोई चीज़ भी पेचीदा नहीं है। आप कोई भी किताब उठाकर देख लें। आपको लगेगा कि बड़ी अक़्ली, साइंटिफ़िक और सिस्टमैटिक चीज़ है। आसान-से-आसान चीज़ भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जिन्होंने उसको पढ़ा न हो। जब पढ़ लिया तो फिर बहुत आसान मालूम होता है। आप दो-चार वर्ष फ़िक़्ह की किताबें पढ़ें, आपको बहुत आसान और बहुत लिबरल और साइंटिफ़िक मालूम होंगी।
सवाल : क्या कुछ लोग इस्लामी फ़िक़्ह को पुन: संकलित कर रहे हैं?
जवाब : इस्लामी फ़िक़्ह का पुन: संकलन तो निरन्तर होता रहता है। कोई दौर ऐसा नहीं आया और न आएगा कि फ़िक़्ह में पुन: संकलन, पुनरावलोकन, revision और re-codification की प्रक्रिया न होती हो। इसलिए कि इंसानी हालात बदलते रहते हैं। इंसान के स्वभाव, समस्याएँ और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जब समस्याएँ और परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हर दौर के फुक़हा अपने दौर के अनुसार समस्याओं पर ग़ौर करते रहते हैं और निर्देश और मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसलिए यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज उसको करने की आवश्यकता पेश आए। यह तो शुरू से हो रही है। कल इंशाअल्लाह उसूले-फ़िक़्ह पर चर्चा होगी। उसूले-फ़िक़्ह तुलनात्मक रूप से ज़रा मुश्किल मज़मून है। और फ़िक़्ह के सबसे मुश्किल लेख में से है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना आसान अंदाज़ में पेश किया जा सके, मैं पेश करूँगा।
Recent posts
-

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -

फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025