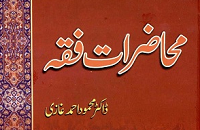
इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह : बुद्धि एवं पुस्तकीय ज्ञान का अनूठा उदाहरण (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 2)
-
फ़िक़्ह
- at 25 December 2024
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
आज की चर्चा का विषय है, उसूले-फ़िक़्ह अर्थात् इस्लामी धर्मशास्त्र का सिद्धांत । यह फ़िक़्हे-इस्लामी का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे अनूठा विभाग है। अगर इल्मे-फ़िक़्ह (धर्मशास्त्रीय ज्ञान) को एक घने, छाँववाले और फलदार वृक्ष से उपमा दी जाए तो उसूले-फ़िक़्ह की हैसियत उस वृक्ष के तने और जड़ों की है। फ़िक़्ह की हैसियत उसकी शाखाओं और आंशिक समस्याओं की हैसियत उस फलदार वृक्ष के फलों और फूल-पत्तों की है।
उसूले-फ़िक़्ह क्या है?
उसूले-फ़िक़्ह से मुराद वे नियम एवं सिद्धान्त और वे उसूल हैं जिनसे काम लेकर एक फ़क़ीह पवित्र क़ुरआन, सुन्नते-रसूल और शरीअत के दूसरे स्रोतों से फ़िक़ही आदेश मालूम करता है और नित्य सामने आनेवाली व्यावहारिक समस्याओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन संकलित करता है। यानी शरीअत के व्यावहारिक आदेशों को उनके विस्तृत तर्कों से मालूम करने में जो नियम-क़ानून सहयोगी और मददगार साबित हों, उन नियम-क़ानूनों के संग्रह का नाम उसूले-फ़िक़्ह है। यह ज्ञान न केवल इस्लामी उलूम में, बल्कि तमाम इंसानी ज्ञान-विज्ञान में एक अनूठी शान रखता है। यह बुद्धि एवं किताबों से अर्जित ज्ञान की विशिष्टता का एक ऐसा अनूठा नमूना है जिसका उदाहरण न केवल इस्लाम के इतिहास में, बल्कि दूसरे ज्ञान-विज्ञान के इतिहास में भी नहीं मिलता।
बुद्धि एवं पुस्तकीय ज्ञान का टकराव और उसूले-फ़िक़्ह
दुनिया के हर धर्म को एक बड़ी पेचीदा और मुश्किल स्थिति का सामना हुआ है। जिससे निबटने में अक्सर धर्म नाकाम रहे हैं। वह मुश्किल यह है कि धार्मिक मामलों में बुद्धि की भूमिका को किस हद तक और कैसे स्वीकार किया जाए और सांसारिक मामलों में धर्म और नैतिक आचरण की भूमिका को किस हद तक जगह दी जाए। कुछ धर्मों और क़ौमों ने इसका समाधान यह निकाला कि विशुद्ध आध्यात्मिक और पारलौकिक मामले धर्म के सिपुर्द कर दिए जाएँ और सांसारिक मामले सारे-के-सारे बुद्धि को सौंप दिए जाएँ। निकट अतीत और सुदूर अतीत में बहुत-से धर्मों ने इस मुश्किल से निबटने का यही रास्ता अपनाया। इसका परिणाम यह निकलता है कि मानव-जीवन को एक न सुलझनेवाली गुत्थी का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप मानव-सभ्यता और संस्कृति को एक घोर नैतिक एवं वैचारिक संकट से दो-चार होना पड़ता है। इस शदीद वैचारिक और नैतिक बोहरान के परिणामस्वरूप एक ज़बरदस्त सांस्कृतिक विनाश और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। मानव-जीवन दो विभागों में विभाजित हो जाता है। एक धर्म का विभाग कहलाता है दूसरा दुनिया का विभाग कहलाता है। और इन दोनों का आपस में कोई सम्पर्क नहीं होता। जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे दुनिया के काम के नहीं रहते, और जो लोग दुनिया में सफल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे धर्म की दृष्टि से असफल ठहरते हैं।
यह मुश्किल दुनिया के हर धर्म को पेश आई। इसको सफलता के साथ और अत्यन्त सन्तुलन और सूक्ष्मता के साथ जिस व्यवस्था ने सुलझाया है, वह शरीअत की व्यवस्था है। जिसमें एक ही समय में बुद्धि की तमाम अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ-साथ शरीअत के दिए हुए सिद्धान्त, यानी अल्लाह की वह्य का मार्गदर्शन पूर्ण रूप से कार्यरत रहता है। इस विशिष्टता और सन्तुलन का अगर कोई सबसे नुमायाँ और सबसे अनूठा नमूना है तो वह उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान है। यह वह ज्ञान है जिसके मौलिक सिद्धान्त, नियम और मौलिक ढाँचा पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से उद्धृत है। गोया धार्मिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक सीमाओं के पालन का मुकम्मल और पूरा-पूरा सामान मौजूद है। जिसमें यह मौलिक और सबसे पहली शर्त आरम्भ से शामिल है कि क़ानून और नियम केवल वह स्वीकार्य होगा, उसके अलावा कोई क़ायदा या क़ानून स्वीकार्य नहीं होगा, जिसका आधार और प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से क़ुरआन और सुन्नत के तर्कों तक पहुँचता हो। इस तरह धार्मिक मार्गदर्शन का पूरा प्रबन्ध यहाँ आरम्भ से मौजूद है। अल्लाह की वह्य (प्रकाशना) का पूर्ण मार्गदर्शन हर-हर सतह और हर-हर क़दम पर मौजूद है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने उदाहरण देकर बताया था कि अगर कोई नियम या क़ायदा पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल से सम्बन्ध न रखता हो वह फ़िक़्ह नहीं कहला सकता। कोई क़ानूनी उसूल या फ़िक़्ह की नियम उसी समय कहलाएगा जब उसकी आधारशिला पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के तर्कों पर रखी गई हो।
दीन और धर्म और वह्य तथा नैतिकता से इस गहरे और वास्तविक जुड़ाव के साथ-साथ उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान की चर्चाओं और लेखों में बुद्धि का कार्यरत होना इस हद तक है कि पूरे ज्ञान की उठान अत्यन्त बौद्धिक और तार्किक ढंग से हुई है। जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, उलमाए-उसूल (सिद्धान्तों के ज्ञाता), मंतिक़ (तार्किकता) और फ़लसफ़ा (दर्शन) के सिद्धान्तों, नियमों और अपेक्षाओं के आधार पर इस कला की इमारत बनाते चले गए, और एक ज़माना ऐसा आया कि बौद्धिक जगत् के किसी बड़े-से-बड़े प्रतिनिधि के लिए यह सम्भव नहीं हुआ कि उसूले-फ़िक़्ह के किसी सर्वमान्य नियम या सिद्धान्त पर उंगली रखकर यह कह सके कि यह चीज़ बौद्धिकता या तार्किकता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।
मुस्लिम बौद्धिकता और उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान
अभी आगे चलकर मैं ज़रा विस्तार से बताऊँगा कि मुसलमानों में बौद्धिकता और तार्किकता में दक्षता, बल्कि इमामत (नेतृत्व) के जो बड़े-बड़े प्रतिनिधि हैं वे ‘उसूल’ के ज्ञान के भी सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। जो तार्किकता और बौद्धिकता का जितना बड़ा माहिर है वह उसूले-फ़िक़्ह का भी उतना ही बड़ा माहिर है। इमाम ग़ज़ाली और इमाम राज़ी के नाम इसकी मिसाल हैं। मुस्लिम जगत् में इमाम ग़ज़ाली और राज़ी का नाम बौद्धिकता में उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। ये दोनों ‘उसूल’ के ज्ञान के भी पहली पंक्ति के इमाम हैं और ‘उसूल’ के ज्ञान की बेहतरीन किताबें इनके क़लम से निकली हैं। ऐसी बेहतरीन किताबें कि आज तक पश्चिमी जगत् उनका उदाहरण पेश नहीं कर सका है। पश्चिम में ‘उसूले-क़ानून’ के ज्ञान की बेहतरीन-से-बेहतरीन किताबें, उदाहरणार्थ रोस्को पाउंड (Roscoe Pound) के लेख भी अपने अत्यन्त बौद्धिक तर्कों, तार्किक सोच की गहराई और लेखन की व्यापकता में इमाम ग़ज़ाली (रह॰) की ‘अल-मुस्तसफ़ा’ और इमाम राज़ी की ‘अल-महसूल’ के बराबर नहीं। इससे आपको यह अनुमान हो जाएगा कि बुद्धि और पुस्तकीय ज्ञान की विशिष्टता का मानव इतिहास में पूर्ण और अद्वितीय नमूना देखना हो तो उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान को देखा जाए।
कुछ आधुनिक लेखकों ने लिखा है कि मुसलमानों की बौद्धिक कार्यप्रणाली यानी intellectual methodology जिस कला में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आती है वह उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान है, जिससे यह पता चलता है कि मुसलमानों का वैचारिक संगठन, मानसिक संरचना और वैचारिक प्रशिक्षण किस ढंग का हुआ है कि एक ही समय में उनकी लगामें बौद्धिकता पर भी हैं और इलाहियात (ईश्वरीय मामलों) और अल्लाह की वह्य की रौशनी से भी वे प्रकाशित हैं। इन दोनों को इस तरह से एक-दूसरे में समोया गया है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक बन गए हैं।
यह है वह उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान, जिसका उद्देश्य यह है कि पवित्र क़ुरआन, सुन्नते-रसूल और इन दोनों के आधार पर फ़िक़्ह और शरीअत के आदेशों के जो मूल स्रोत मान्य हैं, उनसे काम कैसे लिया जाए। उनसे विस्तृत आदेश कैसे निकाले जाएँ। और वह असीम फ़िक़ही संग्रह, वह बेइन्तिहा क़ानूनी दौलत जिसकी हल्की-सी झलक पिछले लेक्चर में आपने देखी थी। इसमें कैसे नई-नई पेश आनेवाली समस्याओं के आधार पर व्यापकता दी जाए। आज स्थिति यह है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) को फ़िक़्ह के आदेश संकलित किए हुए लगभग एक हज़ार वर्ष हो चुके हैं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के देहान्त को साढ़े बारह सौ वर्ष हो चुके हैं। इमाम शाफ़िई (रह॰) के देहान्त को बारह सौ वर्ष हो चुके हैं। इमाम मालिक (रह॰) के देहान्त को सवा बारह सौ वर्ष हो चुके हैं। ये वे सबसे बड़े इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) हैं जिनके समय के और साथ के सैंकड़ों फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन उनके ज़माने में मौजूद थे। इन व्यक्तियों ने अपने सामूहिक प्रयासों से यह संग्रह संकलित किया। इसके लिए उन्होंने ‘उसूले-फ़िक़ह’ के ज्ञान से काम लिया। यह संग्रह आज तक मुसलमानों के काम आ रहा है। आज दुनिया में जितने मुसलमान हैं, वे सब-के-सब बिना अपवाद, इन सबमें किसी-न-किसी की पैरवी कर रहे हैं। कहीं इमाम अहमद-बिन-हंबल के इज्तिहाद की पैरवी हो रही है। कहीं इमाम शाफ़िई (रह॰) के इज्तिहाद पर अमल हो रहा है। कहीं इमाम मालिक (रह॰), अबू-हनीफ़ा (रह॰) और इमाम जाफ़र सादिक़ (रह॰) के दृष्टिकोण पर अमल हो रहा है। इससे यह मालूम हुआ कि इन लोगों ने वह असाधारण चीज़ तैयार कर दी थी कि उम्मते-मुस्लिमा को इसमें बढ़ौतरी या फेर-बदल की बहुत कम आवश्यकता महसूस हुई। अत्यन्त सीमित, बल्कि कुछ अपवाद मामले हैं जिनमें नई समस्याएँ पेश आईं और नए इज्तिहाद की आवश्यकता पड़ी। वरना अधिकतर जो संग्रह इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने तैयार कर दिया, उसके आधार पर मुसलमानों की अरबों-खरबों समस्याएँ हल होती चली जा रही हैं। एक अरब बीस करोड़ मुसलमानों की दिन-प्रतिदिन पेचीदा समस्याएँ आज भी उन्हीं फ़ुक़हा के इज्तिहादात की रौशनी में उन्हीं के संकलित किए हुए नियम-क़ानून और इज्तिहाद और इस्तिंबात (आदेश निकालने) के उसूलों की सहायता और मार्गदर्शन से हल हो रही हैं।
लोग कहते हैं कि मुसलमानों को ज़माने का साथ देना चाहिए। मुसलमान आख़िर क्यों ज़माने का साथ दें? मुसलमानों ने ज़माने का साथ कभी नहीं दिया। मुसलमान कभी ज़माने का साथ नहीं देता। मुसलमान तो ज़माने से आगे होता है और ज़माने का नेतृत्व करता है। इन फ़ुक़हा ने अपने ज़माने का मात्र साथ ही नहीं दिया, मात्र सामयिक समस्याएँ हल करने पर ही ज़ोर नहीं दिया, बल्कि अपने ज़माने से पाँच-पाँच सौ वर्ष बाद की बातें कहीं। एक-एक हज़ार वर्ष आगे की बातें कहीं। और आज हज़ार बारह सौ वर्ष बाद भी लोग उनके काम से मुक्त नहीं हैं। यह कारनामा है उसूले-फ़िक़्ह का कि उसने वह नियम इतनी मज़बूती के साथ और इतने दृढ़ बौद्धिक आधार पर तैयार कर दिए थे कि आज तक उसमें किसी बड़े पुनरावलोकन और मौलिक फेर-बदल की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।
जैसा कि मैंने बताया कि उसूले-फ़िक़्ह वह कला है जिसमें बुद्धि और किताबी ज्ञान दोनों की विशिष्टता पाई जाती है। यहाँ एक तरफ़ क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में नए-नए निकलनेवाले आदेश हैं जो आए दिन संकलित हो-होकर फ़िक़्ह के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ नई-नई निकलनेवाली समस्याएँ और मुश्किलें हैं जिनका समाधान इस कला के ज़रिये शरीअत के स्पष्ट आदेशों से निकाला जा रहा है। इसी पवित्र क़ुरआन और इसी सुन्नत और इन्ही सिद्धान्तों से यह समाधान निकल रहा है। फिर जो शरीअत के स्पष्ट आदेश हैं और जिनकी संख्या अत्यन्त सीमित है, वे असीमित हालात पर चरितार्थ होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद कभी किसी नई स्थिति पर पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेशों को फ़िट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत-सी महत्वपूर्ण और पेचीदा समस्याओं के समाधान के बारे में एक से अधिक रायें मौजूद हैं और आगे भी रायों और व्याख्याओं की यह विविधता मौजूद रहेगी। यह इसलिए कि शरीअत ने अपने स्वभाव और व्यवस्था में एक व्यापकता रखी है कि हर पृष्ठभूमि, हर रहन-सहन और संस्कृति से आनेवाला इंसान अपने परिवेश, व्यवस्था और स्वभाव के अनुसार शरीअत के आदेशों पर अमल कर सके।
उसूले-फ़िक़्ह और इस्लामी सभ्यता की विशेषता
फिर क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में ऐसे विस्तृत नियम-क़ानून इस कला की सहायता से बनाए गए जिन्होंने नई आनेवाली स्थिति में मुस्लिम समाज को हर प्रकार की गुमराही, पेचीदगी और मानसिक उलझनों से बचाया। क़ौमों को मानसिक उलझनें हमेशा पेश आती रही हैं। जब भी किसी क़ौम में कोई बड़ी बदलाव आया, उससे हज़ारों प्रकार की समस्याएँ पैदा हुईं। जब भी किसी क़ौम का तुलनात्मक रूप से किसी दूसरी अधिक सभ्य या ज़्यादा ताक़तवर क़ौम से वास्ता पड़ा, उसके अपनी विचारधारा या तो ख़त्म हो गई या मिट गई या बदल गई। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है और इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं कि एक क़ौम के पास एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी और विकसित समाज था, स्वयं वह क़ौम भी अत्यन्त विकसित थी, लेकिन जब उसका दूसरी क़ौमों से मामला हुआ और दूसरी सभ्यताओं से उसका मेल-जोल हुआ तो उसके विचारों में परिवर्तन आया, उसकी विचारधारा बदल गई, उसकी धारणाओं में एक नया आयाम पैदा हो गया। हिंदुओं को देख लें, वे दुनिया की बहुत प्राचीनतम क़ौमों में से हैं। उनके पास एक प्राचीन दर्शन बहुत संकलित रूप में मौजूद है। धार्मिक ग्रन्थ हैं। विभिन्न ज्ञान-विज्ञान उन्होंने ईजाद किए। गणित जैसी कला उनका आविष्कार है। चिकित्सा का एक विशेष विभाग हिंदुओं का दिया हुआ है। कई हज़ार वर्ष पुरानी चिकित्सा सम्बन्धी परम्पराएँ हिंदुओं के यहाँ चली आ रही हैं। लेकिन जब उनका वास्ता मुसलमानों से पड़ा तो उनके जीवन का हर-हर क्षेत्र इस्लामी शिक्षा और धारणाओं से प्रभावित हुआ। उनके जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा था जो मुसलमानों के प्रभाव से बचा हो। इसके विपरीत दूसरी तरफ़ देखिए। यह बद्दू जो अरब के निर्जल मरुस्थलों से निकले थे। ये रेगिस्तानों में फिरनेवाले जो अरब के रेगिस्तान से निकले तो दुनिया के हर इलाक़े में गए। सीरिया और फ़िलस्तीन जैसे ख़ुशहाल और हरे-भरे इलाक़ों में पहुँचे। रोम और ईरान जैसे बड़े-बड़े और प्राचीन सभ्य साम्राज्य उनके हाथों समाप्त हुए, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ बसनेवाले तमाम लोगों को प्रभावित किया और स्वयं किसी से प्रभावित नहीं हुए। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) जैसे फ़ुक़हा से लेकर इमाम मुस्लिम (रह॰) जैसे मुहद्दिसीन तक इस्लाम के प्रतिनिधियों को देखिए, उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध अरब के बाहर से था। इमाम बुख़ारी (रह॰) और इमाम मुस्लिम (रह॰) मध्य एशिया और ईरान से आए। ये तो अपने साथ कोई विचारधारा लेकर नहीं आए। जो विचारधारा यहाँ से निकली थी उसे ही लेकर गए और दूसरों को प्रभावित किया।
यह मानव इतिहास की एक ऐसी अद्भुत सच्चाई है कि एक ऐसी क़ौम जिसके पास अपनी कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संसकृति नहीं थी, अपनी कोई ज्ञानपरक परम्पराएँ नहीं थीं, उनके पास दुनिया को देने के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर कुछ नहीं था, रेगिस्तानों में घूमते थे, ऊँटों पर सफ़र करते थे और जो कुछ इधर-उधर से मिल जाता था वह खा पी लिया करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की सभ्यताओं को, समाजों को, जीवन पद्धतियों को, शासन व्यवस्थाओं को, क़ानूनों को और हर चीज़ को प्रभावित किया और सिरे से बदलकर रख दिया। दुनिया इनसे प्रभावित हुई, ये किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुए। यह जो प्रभावित करने की शक्ति पैदा हुई, यह कहाँ से पैदा हुई। यह क़ुरआन और सुन्नत की व्याख्या के उन सिद्धान्तों से हुई जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा उसूले-फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञाताओं का है।
क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेश सीमित हैं। आप उनको ज़बानी याद कर सकते हैं। आपको ऐसे सैंकड़ों, बल्कि हज़ारों लोग मिल जाएँगे जिनको वे सारी हदीसें ज़बानी याद हैं जिनसे शरीअत के आदेश निकलते हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हर जगह और हर देश में, बल्कि बस्ती-बस्ती और गाँव-गाँव मिलेंगे जिनको पवित्र क़ुरआन की आयतें मौखिक रूप से कंठस्थ हैं। इन सीमित स्पष्ट आदेशों के विपरीत जितने मामले और समस्याएँ हैं वे असीमित हैं। इन असीमित मामलों के सम्बन्ध में इन सीमित आदेशों पर अमल कैसे हो रहा है? यह एक नियम एवं सिद्धान्त के तहत हो रहा है। यह नियम और सिद्धान्त वह है जिसपर आज चर्चा हो रही है यानी उसूले-फ़िक़्ह। शरीअत के मामलात पर गहन चिन्तन-मनन के नियम। इस गहन चिन्तन-मनन के नियम एवं सिद्धान्त जिनके तहत इस प्रक्रिया को किया जा रहा है।
उसूले-फ़िक़्ह की कलात्मक परिभाषा
उसूले-फ़िक़्ह की कलात्मक परिभाषाएँ उलमाए-उसूल ने बहुत-सी की हैं। जिनमें कोई मौलिक या बुनियादी अन्तर नहीं है। शब्दों के अन्तर के साथ मौलिक बात सबने एक ही कही है। इन सब परिभाषाओं में समानता यह है कि ये वे नियम और आदेश हैं जिनके द्वारा शरीअत के फ़ुरूई यानी आंशिक आदेशों को विस्तृत तर्कों से निकाला जा सके। इस कला का नाम जो इन नियमों एवं आदेशों से बहस करती है, उसूले-फ़िक़्ह है।
उसूले-फ़िक़्ह का उद्देश्य
इस कला के उद्देश्य क्या हैं? मुसलमानों की एक परम्परा यह रही है जिसकी प्राचीन दीनी दर्सगाहों में आज तक पैरवी की जाती है कि जब किसी नए ज्ञान या कला को प्राप्त किया जाए तो सबसे पहले यह देखा जाए कि उस कला का उद्देश्य क्या है। यानी ज्ञान की उद्देश्यपूर्णता पहले क़दम के तौर पर स्वीकार की जाए। निरुद्देश्य और बेफ़ायदा ज्ञान-विज्ञान को सीखने में समय नष्ट न किया जाए, किसी निष्परिणाम या निष्फल गतिविधि को मात्र समय और संसाधन की बरबादी या मात्र मस्तिष्क या शारीरिक विलासिता के लिए अपनाया न जाए, बल्कि केवल ‘इल्मे-नाफ़े’ (लाभकारी ज्ञान) पर ध्यान दिया जाए। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुसलमानों को ‘इल्मे-नाफ़े’ (लाभकारी ज्ञान) की शिक्षा दी और ‘इल्मे-ग़ैर-नाफ़े’ (अलाभकारी ज्ञान) से मुसलमानों को बचने का आदेश दिया। ‘इल्मे-ज़ार’ (हानिकारक ज्ञान) से पनाह माँगी। जिस ज्ञान का कोई दीनी या सांसारिक लाभ न हो और जिससे ज्ञान प्राप्त करनेवाले के व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन को कोई फ़ायदा न हो, उस ज्ञान से अल्लाह के रसूल ने पनाह माँगी है और मुसलमानों को पनाह माँगने का उपदेश दिया है। इस परम्परा का यह परिणाम था कि मुसलमान जब कोई ज्ञान सीखता था तो सबसे पहले यह मालूम करता था कि इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है।
उसूले-फ़िक़्ह का उद्देश्य सबसे बढ़कर अल्लाह की शरीअत पर अमल करके उसकी प्रसन्नता की प्राप्ति है। जब अल्लाह की शरीअत पर इंसान अमल करेगा तो अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह की शरीअत पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि नित्य के मामलों में इंसान को अल्लाह की शरीअत के आदेशों का पता हो। अल्लाह की शरीअत के आदेश जानने के लिए ज़रूरी है कि मुझे यह मालूम हो कि पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से विस्तृत आदेश कैसे निकाले जाएँ। इन विस्तृत आदेशों को जानने के लिए उसूले-फ़िक़्ह का जानना ज़रूरी है। इसलिए उसूले-फ़िक़्ह का पहला उद्देश्य तो अल्लाह की प्रसन्नता की प्राप्ति है। दूसरा उद्देश्य दुनिया और आख़िरत में सफलता और कामयाबी है, जिसके लिए पवित्र क़ुरआन ने क्रमशः ‘सलाह’ और ‘फ़लाह’ की शब्दावलियाँ प्रयुक्त की हैं। ‘सलाह’ इस दुनिया में सफलता और ‘फ़लाह’ उस दुनिया में सफलता।
उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान का आरम्भ
उसूले-फ़िक़्ह का आरम्भ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के शुभ हाथों से हुआ। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने वे नियम-क़ायदे तैयार किए जिनके आधार पर आगे चलकर उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान अस्तित्व में आया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का इस ज्ञान के नियम तैयार करने और इसकी बुनियादें रखने में कितना हिस्सा है, इसके विस्तृत उदाहरण देना तो मुश्किल है, लेकिन दो-तीन उदाहरण मैं बताता हूँ।
उसूले-फ़िक़्ह का एक उसूल यह है कि जब आप कोई आदेश मालूम करें या किसी मामले में शरीअत का पक्ष जानना चाहें, तो जो राय आपने समझी है और पवित्र क़ुरआन या सुन्नत की किसी ‘नस्स’ (स्पष्ट आदेश) से शरीअत का जो आदेश आपकी समझ में आया है, उसके बारे में यह भी देख लें कि इसपर अमल करने से अन्ततः परिणाम क्या निकलेगा। अगर परिणाम वही निकलेगा जो शरीअत का उद्देश्य है तो आपका इज्तिहाद (राय) दुरुस्त है। और अगर परिणाम वह निकले जो शरीअत का उद्देश्य नहीं तो उसका मतलब यह है कि आपसे इज्तिहाद में कोई ग़लती हुई है। आप दोबारा ग़ौर करें। इसलिए कि शरीअत के किसी आदेश का नकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता। इसी तरह अगर आप यह जानना चाहें कि कोई कार्य जिसका कोई निश्चित और स्पष्ट आदेश पवित्र क़ुरआन या सुन्नते-रसूल में नज़र न आता हो उसके वैध या अवैध होने के लिए यह भी देखा जाए कि इस कार्य के क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उसूल है उसूले-फ़िक़्ह का। इसको प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने खोजा है। हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह उसूल खोजा था। खोजने से मेरी मुराद यह नहीं जिस तरह वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठे विज्ञान के उसूल की खोज करता है, बल्कि मेरी मुराद यह है कि सबसे पहले यह उसूल इतने स्पष्ट रूप से उनके ज़ेहन में आया। उनका जीवन क़ुरआन एवं हदीस के अध्ययन और उसके सन्देश एवं तत्वदर्शिता पर चिन्तन-मनन में बीता। उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी पूरी उम्र जवानी और उधेड़ावस्था तक अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ में गुज़ारी। फिर उसके बाद भी पवित्र क़ुरआन और सुन्नत पर ग़ौर करते रहे। इस चिन्तन-मनन के परिणामस्वरूप उनको जो समझ और अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई, उसके आधार पर उन्होंने यह मूल कुल्लिया (सिद्धान्त) बनाया, जिससे शेष सहाबा ने सहमति जताई।
मसला यों पैदा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने तक शराब पीने की कोई निर्धारित सज़ा नहीं थी। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में एक-दो घटनाओं में शराब पीने की शिकायत हुई। किसी ने किसी ग़लत-फ़हमी में या शैतान के बहकावे में आकर शराब पी ली। जब इस तरह की कोई घटना अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में लाया गया तो उन्होंने फ़रमाया कि सज़ा दे दो। कभी फ़रमाया कि चालीस कोड़े मॉरो, कभी डाँटकर वापस कर दिया, कभी धमकाकर वापस कर दिया और कभी अस्सी कोड़ों की सज़ा दी। लेकिन कोई अन्तिम (Final) सज़ा निर्धारित नहीं की। एक बार एक साहब चौथी बार शराब पीने के आरोप में लाए गए, तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को सख़्त नागवार गुज़रा और उन्होंने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! यह बार-बार पीता है, मैं इसको क़तल न कर दूँ?” अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह सुनकर मुस्कराए और कहा कि “यह शख़्स अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता है।” यानी एक सहाबी के बारे में उन्होंने कहा कि चूँकि यह अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता है इसलिए उनकी इस कमज़ोरी और ग़लती के बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया। उन साहब ने यह वाक्य सुनने के बाद पूरे जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया।
जब हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का ज़माना आया तो बहुत-सी नई-नई क़ौमें इस्लाम में दाख़िल हुईं। ईरानी, सीरियाई और मिस्री वग़ैरा। उनमें से कुछ को इस्लाम के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था कुछ को नहीं किया गया था। कुछ का प्रशिक्षण अभी हो ही रहा था। ऐसे में शराबनोशी की घटनाएँ बहुत अधिक होने लगीं। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को बुलाकर मश्वरा किया, और कहा कि यह तो बड़ी चिन्ताजनक बात है कि शराब पीने की घटनाएँ इतनी अधिक हो रही हैं। इसकी कोई निर्धारित और सख़्त सज़ा होनी चाहिए। हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा, “जब शराब पिएगा तो नशे में मुब्तला होगा” और “जब नशा आएगा तो फ़ुज़ूल बातें करेगा और ऊट-पटाँग बकेगा। और जब ऊट-पटाँग बकेगा तो किसी पर आरोप भी लगाएगा। और जब आरोप लगाएगा तो अस्सी कोड़ों की सज़ा पाएगा। अत: मेरे ख़याल में शराब पीने की सज़ा अस्सी कोड़े होनी चाहिए।” सब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस तर्क से सहमति जताई और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने शराब पीने की सज़ा अस्सी कोड़े निर्धारित की। यह एक उदाहरण है कि एक बड़े सहाबी ने दूसरे सहाबा के मतैक्य से एक उसूल बनाया कि किसी मामले का फ़ैसला करते हुए यह भी देखा जाएगा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम अच्छा निकलेगा तो मामला अच्छा है और अगर परिणाम बुरा निकलेगा तो मामला बुरा है।
हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास एक साहब आए और इद्दत का एक मसला पूछा। पवित्र क़ुरआन में इद्दत के बारे में तीन आयतें आई हैं। एक आयत में यह है कि अगर किसी महिला के पति का देहान्त हो जाए तो वह चार महीने दस दिन प्रतीक्षा करे। एक जगह आया है कि जिस महिला को तलाक़ हो जाए वह तीन पीरियड (तीन बार मासिक धर्म आने) तक प्रतीक्षा करे। एक जगह आया है कि जिस महिला को गर्भावस्था में तलाक़ हो जाए तो जब तक उसके यहाँ बच्चे का जन्म न हो उस समय तक प्रतीक्षा करे। ये तीन आयतें विभिन्न समयों और विभिन्न स्थितियों के बारे में आई हैं। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास आनेवाले व्यक्ति ने एक ऐसी महिला की तलाक़ का मसला पूछा जिसके यहाँ बच्चा भी पैदा होनेवाला था और उसके पति का देहान्त भी हो गया था। अब दो विभिन्न आयतों में दो अलग-अलग आदेश आए हैं। विधवा की इद्दत का आदेश एक आयत में है और बच्चे के जन्म का दूसरी आयत में है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जवाब में कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि सूरा अत-तलाक़ सूरा अल-बक़रा के बाद नाज़िल हुई थी।
सुननेवाले ने सुन लिया और समझनेवाले ने समझ लिया कि वे यह कह रहे हैं कि बाद की आयतों की रौशनी में पहले की आयतों को देखा जाएगा। पहली आयतों की व्याख्या करते हुए बादवाली आयत को सामने रखा जाएगा। पवित्र क़ुरआन की किसी एक आयत को अलग से देखकर फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि इस विषय को देखकर बाद में आनेवाली दूसरी उसी विषय की आयतों की रौशनी में उसके अर्थ को समझा जाएगा और वह किन मामलों पर फ़िट होती है, यह तय किया जाएगा। आज दुनिया की हर क़ानूनी व्यवस्था में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि क़ानून की किसी धारा का वास्तविक उद्देश्य और अर्थ निर्धारित करने के लिए उन सभी धाराओं को देखा जाए जो बाद में इस विषय पर आई हैं। क़ानून की एक इबारत है जो आम तौर से जज महोदयों के फ़ैसलों में बहुत अधिक प्रयुक्त होती है to be read with, फ़ैसले में जज लिखता है कि—
Under section such-and-such of the Pakistan Penal Code, read with section such-and-such.
यानी “मैं यह फ़ैसला करता हूँ कि अमुक धारा को अमुक धारा के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और इन दोनों को अमुक क़ानून की अमुक धारा के साथ पढ़ा जाए।” इसकी रौशनी में यह आदेश क़रार दिया जाता है। आज दुनिया की हर अदालत में इस नियम को प्रयुक्त किया जाता है। इस नियम के जनक हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं।
इस तरह से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने विभिन्न समयों में विभिन्न उसूल और क़ायदे मुक़र्रर किए। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास एक महिला आई और कहा कि मेरे बाल छोटे हैं या उड़ गए हैं। मैं अमुक जगह गई, वहाँ किसी महिला के कटे हुए बाल बिक रहे थे। मैं वे ख़रीद कर ले आई हूँ और अपने सिर में लगाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह दुरुस्त नहीं है। आप मुझे अल्लाह की किताब के अनुसार इसका फ़ैसला बताएँ कि क्या है। अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि अल्लाह की किताब में इसकी मनाही आई है। वह महिला चली गई। लेकिन कुछ दिन के बाद आकर कहने लगी कि मैंने तो अल्लाह की किताब पूरी पढ़ ली है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि किसी के बाल लेकर अपने सिर में मत लगाओ। जवाब में अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि “अगर तुम उसको आँखें खोलकर पढ़तीं तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब साफ़-साफ़ नज़र आ जाता। उन्होंने कहा कि आप ही बता दीजिए। जवाब दिया कि पवित्र क़ुरआन में आया है कि ‘जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दे दें वह ले लो और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ’। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला उन औरतों पर लानत फ़रमाए जो अमुक-अमुक और अमुक काम करती हैं और दूसरी औरतों के बाल अपने सिर में लगाती हैं।”
गोया हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) यह आदेश दे रहे थे कि पवित्र क़ुरआन में कोई आदेश ऐसा नहीं है जो सुन्नत के आदेश से टकराता हो। और इसी तरह सुन्नत में कोई आदेश ऐसा नहीं जिसका कोई आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र क़ुरआन में मौजूद न हो। पवित्र क़ुरआन सुन्नत के आदेशों का आधार है, और सुन्नत पवित्र क़ुरआन के आदेश की व्याख्या है। जहाँ सुन्नत में विस्तार है उसका संक्षिप्त आदेश क़ुरआन में होगा, और इसी तरह जहाँ क़ुरआन में विस्तार है उसका संक्षिप्त आधार सुन्नत में होगा। ये दोनों-एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इस तरह की मिसालें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात और कथनों से जमा की जाएँ तो वे सैंकड़ों, बल्कि शायद हज़ारों की संख्या में होंगी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अपने अद्वितीय प्रशिक्षण और दीनी (धार्मिक) अन्तर्दृष्टि से काम लेकर ऐसे उसूल बनाए हैं, जिनसे ताबिईन लाभान्वित हुए। स्वयं ताबिईन ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के मुबारक हाथों प्रशिक्षण पाया, प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात (रायों) को जमा किया, उनको लिखित रूप में संकलित किया, और स्वयं भी इस काम को आगे बढ़ाया। यों ताबिईन ने भी बहुत-से उसूल बनाए।
कभी-कभी ऐसा हुआ, और ऐसा हो सकता है और होता भी है कि बज़ाहिर एक ‘नस्स’ (क़ुरआन या हदीस के स्पष्ट आदेश) का एक अर्थ और एक दूसरी ‘नस्स’ का दूसरा अर्थ हो। और पढ़नेवाले को दोनों में कोई टकराव महसूस हो। इस टकराव को कैसे दूर किया जाएगा। पवित्र क़ुरआन की आयात में तो उमूमन ऐसा नहीं होता। लेकिन हदीसों के मामले में कभी-कभी ऐसा हो जाता है। चुनाँचे पवित्र क़ुरआन की एक आयत है जिसमें एक बड़ी स्पष्ट स्थिति बयान की गई है कि जिन औरतों को तलाक़ हो जाए तो उन्हें तलाक़ देनेवाले पति की तरफ़ से ‘मताअ’ यानी साज़ो-सामान मिलेगा जिसका निर्धारण मारूफ़ (प्रचलित नियम) के अनुसार होगा, और जिसकी निर्धारित अवधि है। इसकी व्याख्या यह है कि इद्दत के दौरान तलाक़-शुदा महिलाओं की सारी ज़िम्मेदारी, गुज़ारा-भत्ता हर चीज़ उनके उस पति के ज़िम्मे है जिसने उनको तलाक़ दी है।
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में इस तरह की एक घटना घटित हुई। तलाक़-शुदा महिला ने इद्दत के दौरान गुज़ारे-भत्ते की माँग की और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की अदालत में फ़रियाद की। उन्होंने इस आयत के अनुसार फ़ैसला किया कि तुम्हें इद्दत के दौरान गुज़ारा-भत्ता रिवाज के मुताबिक़ मिलेगा। इसपर एक और महिला सहाबिया, जो वहाँ मौजूद थीं, खड़ी हुईं और कहा कि मुझे मेरे पति ने तलाक़ दे दी थी। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जानकारी में यह बात आई थी। उन्होंने मुझे न तो किसी गुज़ारा दिए जाने का आदेश दिया और न मेरे लिए किसी आवास का फ़ैसला किया। गोया वह महिला हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस फ़ैसले को सुन्नत के ख़िलाफ़ क़रार देकर उससे अपना मतभेद प्रकट कर रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इसके जवाब में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की मौजूदगी में कहा कि “हम अल्लाह की किताब को और उसके रसूल की सुन्नत एक महिला के बयान के आधार पर नहीं छोड़ सकते जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि उसे सही याद रहा कि नहीं याद रहा।” गोया एक महिला सहाबिया ने बड़े प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के सामने एक हदीस बयान की। वह महिला स्वयं भी सहाबिया हैं और उनके बारे में ग़लत-बयानी या अल्लाह की पनाह झूठ की कोई सम्भावना नहीं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और दूसरे बड़े सहाबा ने इस बयान को अपनी समझ के अनुसार पवित्र क़ुरआन से टकराते समझा और उसे स्वीकार नहीं किया। यों शरीअत की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण उसूल तैयार हुआ कि अगर ऐसी कोई रिवायत बयान की जाए जिसको बयान करनेवाला एक ही रावी हो और वह रिवायत बज़ाहिर पवित्र क़ुरआन के किसी आदेश से टकराते मालूम होती हो, तो इस रिवायत पर अमल नहीं किया जाएगा और यह माना जाएगा कि रावी से कोई भूल-चूक हो गई है। यह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का कहना था और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने उसको माना।
याद रखिएगा कि इस तरह का फ़ैसला करना बड़ी असाधारण ज़िम्मेदारी की बात है। यह फ़ैसला करने के लिए कि कोई हदीस पवित्र क़ुरआन से टकराती है असाधारण अन्तर्दृष्टि, विस्तृत ज्ञान और दक्षता दरकार है। हर ऐरा-ग़ैरा और हम और आप जैसे लोगों का यह काम नहीं है कि कहें कि यह हदीस इस दर्जे की और इस दर्जे की नहीं है। हदीसों के बारे में हदीस के इमामों और मुज्तहिदीन के दर्जे के विद्वानों और विशेषज्ञों ने जो फ़ैसला किया हो उसको मान लेना चाहिए। बहरहाल यह एक उसूल है जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की मौजूदगी में तय किया। इस तरह के उसूल प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने में संकलित होते गए। ताबिईन उनसे लाभान्वित होते गए। ताबिईन के ज़माने में इन सिद्धान्तों को संकलित किए जाने का काम शुरू हुआ, और लिखित रूप से उनके संग्रह तैयार हुए।
उसूले-फ़िक़्ह को सबसे पहले कब संकलित किया गया
सबसे पहले किस फ़क़ीह ने इस विषय पर क़लम उठाया। इसपर इतिहासकारों और संस्मरण लेखकों ने बहुत कुछ चर्चा की है। ज़ाहिर है यह बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात थी कि किसी को उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान पर किताब लिखने में पहला स्थान प्राप्त हो। पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से आदेश निकालने के उसूल हमेशा-हमेशा के लिए संकलित कर देना कोई मामूली सम्मान की बात नहीं है। इसलिए हर फ़क़ीह के पैरोकारों ने यह चाहा कि यह सम्मान उनके इमाम को प्राप्त हो। चुनाँचे शीया लोगों का कहना है कि सबसे पहले इमाम मुहम्मद बाक़िर (रह॰) ने अपने शागिर्दों (शिष्यों) को एक इबारत डिक्टेट कराई थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी समस्याओं पर विचार व्यक्त किए थे जो उसूले-फ़िक़्ह के प्रकार के थे।
इसी तरह का एक लेख्य जो शीया लोगों के पास मौजूद है उनकी किताबों में बहुत ज़्यादा बयान भी होता है। वह इसको इमाम जाफ़र सादिक़ (रह॰) से जोड़ते हैं। शीया विद्वानों के बयान के अनुसार इमाम जाफ़र सादिक़ (रह॰) ने आठ-दस पृष्ठ की एक संक्षिप्त इबारत डिक्टेट कराई थी। इसमें उसूले-फ़िक़्ह की कुछ मौलिक समस्याएँ चर्चा में आई हैं।
हनफ़ी फ़ुक़हा का ख़याल यह है कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने एक किताब संकलित की थी जिसका नाम ‘किताबुर-राय’ था और इसमें यह बयान किया गया था कि इज्तिहाद से कैसे काम लिया जाए और क़ुरआन और सुन्नत की समझ में इंसानी राय का किस हद तक दख़ल है। लेकिन इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) से सम्बन्धित यह किताब आज हमारे पास मौजूद नहीं है। इतिहासकारों ने बयान किया है तो दुरुस्त ही बयान किया होगा। सम्भव है कि इमाम साहब ने ऐसी कोई किताब लिखी हो। लेकिन जिस फ़क़ीह को यह बेमिसाल सौभाग्य प्राप्त है कि उसने उसूले-फ़िक़्ह पर सबसे पहले बाक़ायदा किताब लिखी और आज उसकी लिखी हुई किताब दुनिया-भर में उपलब्ध भी है, और उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, फ़्रांसीसी, फ़ारसी और दुनिया की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद भी मौजूद हैं, वह इमाम मुहम्मद-बिन-इदरीस अश-शाफ़िई (रह॰) हैं जिनकी किताब ‘अर-रिसाला’ उसूले-फ़िक़्ह के विषय पर प्राचीनतम किताब है। इमाम शाफ़िई (रह॰) से पहले की कोई बाक़ायदा और संकलित किताब उसूले-फ़िक़्ह के विषय पर मौजूद नहीं है। इसलिए यह बात बिना किसी डर के कही जा सकती है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) ही उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान के जनक और सबसे पहले संकलनकर्ता हैं।
पश्चिमी इतिहासकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) ही उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान के पहले जनक हैं। एक पश्चिमी इतिहासकार ने लिखा है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) को उसूले-फ़िक़्ह का ज्ञान से वही सम्बन्ध है जो हकीम अरस्ता तालीस को तार्किकता के ज्ञान से है। जिस तरह अरस्तु तार्किकता का आविष्कारक है उसी तरह इमाम शाफ़िई (रह॰) उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान के आविष्कारक हैं। एक और पश्चिमी लेखक ने इमाम शाफ़िई (रह॰) के बारे में लिखा है कि—
He is the greatest systematizer of jurisprudential thought in Islam.
“वे इस्लाम में उसूले-फ़िक़्ह के सबसे बड़े व्यवस्थितकर्ता हैं” यानी उनको व्यवस्था प्रदान करनेवाले हैं। इस दृष्टि से मानवता जगत् को, मैं मुस्लिम जगत् नहीं कह रहा, इमाम शाफ़िई (रह॰) का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा ज्ञान और कला मानवता को प्रदान की जिससे मानवता इमाम शाफ़िई (रह॰) से पहले परिचित नहीं थी। दुनिया की किसी क़ौम में, किसी क़ानून में, किसी सभ्यता और किसी संस्कृति में उसूले-क़ानून या उसके विकल्प के रूप में किसी नाम से कोई कला उस समय मौजूद नहीं थी जब इमाम शाफ़िई (रह॰) यह किताब लिख रहे थे। जब इमाम शाफ़िई (रह॰) के बाद बड़े इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) उसूले-फ़िक़्ह पर किताबें लिख रहे थे जिनमें से कुछ का ज़िक्र मैं अभी करूँगा, उस समय पूरी दुनिया इस कला से अनभिज्ञ थी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि दुनिया का प्राचीनतम क़ानून हम्मूराबी का संकलित किया हुआ है जो 1750 ई॰पू॰ में लिखा गया। फिर प्राचीनतम क़ानूनों में यहूदी क़ानून हैं जो हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के कुछ सौ वर्ष बाद संकलित होने शुरू हुए। फिर रोमन लॉ है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बचपन और आपके दुनिया में आने से थोड़ा-सा पहले लिखा गया। हिन्दू क़ानून है जिसके बारे में विभिन्न दावे हैं कि वह कितना प्राचीन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह प्राचीन ज़रूर है। उनमें से किसी क़ानून के पास उसूले-क़ानून नाम की कोई कला मौजूद नहीं थी। क़ानूनों यानी आंशिक मार्गदर्शन और फ़ुरूई (आंशिक) आदेश तो मौजूद थे जिसके लिए क़ानून की एक शब्दावली है Corpus Juris. तो कॉर्प्स जूरिस यानी Body of the Law तो मौजूद थी। आंशिक आदेश और रोलिंग्ज़ का संग्रह तो मौजूद था, लेकिन इस पूरे संग्रह को व्यवस्थित ढंग से कैसे देखा जाए, इसके नियम क्या हों, उनकी व्याख्याएँ कैसे की जाएँ, इन नियमों को खोजा कैसे जाए, उनके पीछे प्रमाण क्या होगा, कौन-सा नियम सही होगा और कौन-सा ग़लत होगा, इसका कोई उसूल होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ दुनिया के पास मौजूद नहीं थी। और अगर हम थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि 1750 ई॰पू॰ दुनिया में संकलित क़ानून के आरम्भ का इतिहास है, अगरचे संकलित क़ानून का आरम्भ इससे पहले हो चुका था, लेकिन चूँकि प्राचीनतम उदाहरण हम्मूराबी के कोड का है इसलिए हम उससे आरम्भ कर लेते हैं। गोया 1750 ई॰पू॰ से लेकर और लगभग 1750 बाद मसीह तक यानी लगभग 35 सौ वर्ष तक दुनिया के पास उसूले-क़ानून नाम की कोई कला मौजूद नहीं थी। पश्चिमी दुनिया में यह कला पिछले डेढ़ दो सौ वर्षों में पैदा हुई। ज़्यादा सावधानी के तौर पर हम मान लेते हैं कि पश्चिम में यह कला ढाई सौ वर्ष पहले अस्तित्व में आई होगी। इससे पहले पश्चिमी जगत् उसूले-क़ानून नाम की किसी भी कला से अनजान था। हिन्दू आज भी अनजान हैं। हम्मूराबी का क़ानून तो अपनी मौत आप मर गया। रोमन लॉ भी अपनी मौत आप मर गया। दुनिया के अत्यन्त सभ्य क़ानून भी उसूले-क़ानून के नाम से, जिसको आप आंशिक रूप से उसूले-फ़िक़्ह के समान क़रार दे सकते हैं, अनजान थे। यों समष्टीय रूप से पूरी सभ्य और असभ्य दुनिया उसूल-क़ानून के ज्ञान से अनजान थी।
इमाम शाफ़िई (रह॰) की किताब ‘अर-रिसाला’
इमाम शाफ़िई (रह॰) ने क़ानून जगत् की इस धारणा की तरफ़ आने से बारह सौ वर्ष पहले किताब ‘अर-रिसाला’ लिख दी थी और यह किताब मुस्लिम जगत् में आरम्भ से आम हो गई थी। इसलिए यह मुसलमान फ़ुक़हा की सामान्य रूप से और इमाम शाफ़िई (रह॰) की विशेष रुप से इतनी बड़ी देन है कि कानून जगत् उनके उपकार का हमेशा आभारी रहेगा कि पूरी इस्लामी दुनिया को उन्होंने क़ानून के एक नए कला-विभाग से परिचित कराया। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने जब किताब ‘अर-रिसाला’ लिख दी तो पूरी दुनिया में यह एक लोकप्रिय किताब बन गई। किताब ‘अर-रिसाला’ में उसूले-फ़िक़्ह की मौलिक समस्याओं से बहस की गई है। इसमें यह बताया गया है कि मुसलमानों के लिए क़ानूनों के स्रोत कौन-कौन-से हैं। पवित्र क़ुरआन, सुन्नते-रसूल, इजमा (तमाम मुस्लिम विद्वानों का मतैक्य) और क़ियास (इस्लाम के सिद्धान्तों के आधार पर किसी समस्या का अनुमानित समाधान ढूँढ़ना)। उनका इमाम शाफ़िई (रह॰) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया है। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने यह बताया है कि क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेशों की व्याख्या कैसे की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी ख़बरे-वाहिद या किसी दूसरी हदीस में टकराव महसूस हो तो इस टकराव को कैसे दूर किया जाए। पवित्र क़ुरआन की दो आयतें बज़ाहिर टकराती मालूम हों तो इस टकराव को कैसे दूर किया जाए। ये वे समस्याएँ हैं जो इमाम शाफ़िई (रह॰) ने अपनी किताब में उठाई थीं। फिर इमाम शाफ़िई (रह॰) ने यह भी बताया कि स्वयं उन्होंने फ़िक़्ह का जो संपादन किया है और जो आज उनकी किताब ‘किताबुल-उम्म’ में मौजूद है, वह उन्होंने किन उसूलों और किन नियमों के आधार पर किया है। इमाम शाफ़िई (रह॰) की इस किताब के बाद मुस्लिम जगत् के हर इलाक़े में उसूले-फ़िक़्ह पर किताबें लिखी गईं और बहुत जल्द, देखते-ही-देखते, दो ढाई सौ वर्ष के अन्दर-अन्दर एक ऐसी संकलित, परिपूर्ण, गहरी और ठोस कला बन गई जिसका आज भी पश्चिमी जगत् में कोई उदाहरण मौजूद नहीं है।
यह बात मैं किसी अतिशयोक्ति के तौर पर नहीं कह रहा या किसी की श्रद्धा के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि एक वास्तविकता का प्रदर्शन कर रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि आज दुनिया में जो किताबें क़ानून के उसूलों पर लिखी जा रही हैं, उनके बड़े-बड़े प्रतिनिधि जो आज दुनिया में मशहूर हैं, उनकी किताबें अगर उलमाए-उसूल की किताबों के सामने रखी जाएँ तो क़ानून के ये बड़े-बड़े चिन्तक और लेखक मात्र बच्चे मालूम होते हैं। इस गहराई के मुक़ाबले में जो उलमाए-उसूल के यहाँ मिलती है, उनकी हैसियत बच्चे जैसी भी नहीं है। इसके उदाहरण मैं आगे चलकर दूँगा।
जब यह कला लोकप्रिय कला बन गई और मुसलमानों में बड़े-बड़े लोग जो बुद्धि और विवेक में मानव इतिहास में भी नुमायाँ स्थान रखते थे, उन्होंने अपना ध्यान इस कला की ओर लगा लिया, तो तेज़ी के साथ मुस्लिम जगत् में यह कला फैलनी शुरू हुई। एक तरफ़ टीकाकार इल्मे-तफ़सीर के भंडार संकलित कर रहे थे। इसपर किताबें आ रही थीं। गोया क़ानून के एक स्रोत की तैयारी हो रही थी। दूसरी तरफ़ मुहद्दिसीन इल्मे-हदीस के भंडार संकलित कर रहे थे। क़ानून का दूसरा स्रोत तैयार हो रहा था। तीसरी तरफ़ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) इज्तिहादात (रायों) से काम ले रहे थे। नई समस्याओं पर रूलिंग्ज़ सामने आ रही थीं और इस्लाम का अद्वितीय न्यायविधान-संग्रह (Corpus Juris) तैयार हो रहा था। चौथी ओर उलमाए-उसूल इन तीनों स्रोतों से काम लेकर आदेश निकालने के उसूल तैयार कर रहे थे।
उसूले-फ़िक़्ह की दो मुख्य विधियाँ एवं शैलियाँ
उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान को अस्तित्व में आए ज़्यादा समय नहीं गुज़रा था कि इस्तिंबात (आदेश निकालने) के उसूल तैयार करने के दो तरीक़े मुसलमानों में प्रचलित हुए। आपमें से जिनको ‘मंतिक़’ (तार्किकता) के अध्ययन का मौक़ा मिला हो, उनको पता होगा कि दुनिया में तार्किकता की दो महत्वपूर्ण और बड़ी-बड़ी शैलियाँ यानी methods प्रचलित हैं। एक शैली कहलाती है मंतिक़े-इस्तक़राई (निगमनात्मक तार्किकता), दूसरी शैली कहलाती है मंतिक़े-इस्तिख़राजी (आगमनात्मक तार्किकता) यानी deductive logic और inductive logic। इस्तिख़राजी मंतिक़ (तार्किकता) से मुराद सीधी-सादी भाषा में यह है कि पहले सोचकर, एक बौद्धिक तर्क के द्वारा कुछ अलग उसूल सोचे जाएँ, ग़ौर करके तलाश किए जाएँ। फिर इन अलग सिद्धान्तों की रौशनी में आंशिक आदेशों और समस्याओं को मालूम किया जाए। यह मंतिक़े-इस्तिख़राजी का उसूल है। इसकी स्थापना का श्रेय यूनानियों के सिर है और इसका पहला आविष्कारक अरस्तू है। मुसलमानों ने उससे भी लाभ उठाया और उसपर बहुत-सी बहुमूल्य और अनमोल किताबें लिखीं। लेकिन तार्किकता की एक दूसरी शैली वह है जो पवित्र क़ुरआन की वर्णन-शैली और तर्क-शैली से स्वयं मुसलमानों ने खोजी। यह मंतिक़े-इस्तिक़राई की शैली है। आसान भाषा में मंतिक़े-इस्तिक़राई का तरीक़ा यह है कि पहले आंशिक रूप से बहुत-सी मिलती-जुलती घटनाओं को जमा किया जाए। फिर उन घटनाओं में अगर कोई साझा सिद्धान्त कार्यरत है उसको खोजा जाए। इस तरह जुज़इयात (आंशिक बातों) से उसूल जमा किए जाएँ। गोया कुल्लियात (मूल सिद्धान्तों) से जुज़इयात की तरफ़ आने का नाम इस्तिख़राज है, और जुज़इयात से कुल्लियात की तरफ़ जाने का नाम इस्तिक़रा है।
उलमाए-उसूल ने इन दोनों तरीक़ों और शैलियों से काम लिया। एक तरीक़ा कहलाता है तरीक़ा-ए-जमहूर, या तरीक़ा-ए-मुतकल्लिमीन या तरीक़ा-ए-शाफ़ेईया। ये तीनों एक ही विधि के नाम हैं। इस विधि को तरीक़ा-ए-शाफ़ेईया इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले शाफ़िई फ़ुक़हा ने इससे काम लिया। तरीक़ा-ए-मुतकल्लिमीन इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस शैली पर किताबें लिखीं वे उलमाए-उसूल होने के साथ-साथ मुतकल्लिमीन (इस्लामी अक़ीदों पर चर्चा करनेवाले) भी थे। इल्मे-कलाम के विशेषज्ञ भी थे। तरीक़ा-ए-जमहूर इसलिए कहा जाता है कि उलमाए-मालिकिया, शाफ़ेईया और हनाबिला, तीनों ने इस शैली से काम लिया। गोया फ़ुक़हा की अधिक संख्या (जमहूर) ने इस शैली को परवान चढ़ाया।
तरीक़ा-ए-जमहूर
तरीक़ा-ए-जमहूर यह है कि पहले पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेशों पर ग़ौर करके मौलिक सिद्धान्त जुटाए जाएँ। फिर इन मौलिक सिद्धान्तों को फ़िक़ही जुज़इयात पर चस्पाँ किया जाए। जब वे फ़िक़ही स्पष्ट आदेश इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सही साबित हो जाएँ फिर उनको फ़ाइनल समझा जाए और किताबों में लिखा जाए। इस उसूल के अनुसार जो किताबें लिखी गईं, वे मुतकल्लिमीन या तरीक़ा-ए-शाफ़ेईया की किताबें कहलाती हैं। इन किताबों में चार किताबें बड़ी मशहूर हैं जिनके बारे में इब्ने-ख़लदून ने लिखा है कि यह ‘उसूल’ के ज्ञान के चार मौलिक स्तम्भ हैं। वे किताबें ये हैं—
- किताबुल-मुअतमिद
- किताबुल-बुरहान
- अल-मुस्तसफ़ा
- किताबुल-अह्द
इन चार किताबों से प्रभावित होकर इस शैली पर बाद की सदियों में बहुत-सी छोटी-बड़ी किताबें लिखी गईं। मैं अरबी किताबों के और ज़्यादा भारी भरकम नाम लेकर आपको बोझिल नहीं करूँगा। लेकिन इस विषय पर जो किताबें हैं उनकी संख्या दर्जनों से बढ़कर सैंकड़ों में है जो पहली दो तीन सदियों में लिखी गईं। इन सब किताबों की शैली यह है कि पहले वे अपने मौलिक सिद्धान्त बयान करती हैं जिसमें तार्किकता और दर्शन दोनों से काम लेते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा और शैली सामने रखते हैं। पवित्र क़ुरआन अरबी भाषा में है। उसकी व्याख्या में अरबी भाषा के नियमों और शैलियों से काम लेना अपरिहार्य है। अरबी भाषा में भाषा की समझ के जो उसूल हैं, पवित्र क़ुरआन में वे अनिवार्य रुप से दृष्टिगत रखे जाएँगे। यह नहीं हो सकता कि पवित्र क़ुरआन की टीका लिखी जा रही हो और अंग्रेज़ी ग्रामर के अनुसार हो। हदीस की व्याख्या हो और उर्दू ग्रामर के अनुसार हो। वह अरबी भाषा ही के ग्रामर और शैली के अनुसार होगी। इसलिए वर्णन-शैली और भाषा के नियमों की समस्या उसूले-फ़िक़्ह के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से है। अरबी शैली और भाषा एवं वर्णन के जो मामलात उसूले-फ़िक़्ह में चर्चा में आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या स्वयं ‘लफ़्ज़ियात’ और शब्द भंडार यानी vocabulary की है, यानी किस शब्द का क्या अर्थ है। अरबी भाषा में कौन-से शब्द साझे हैं। मजाज़ (सांकेतिक रूप) कहाँ प्रयुक्त होता है, वास्तविक अर्थ कहाँ अभीष्ट होता है। ये सारी बहसें उसूले-फ़िक़्ह में शामिल हो जाती हैं। अत: उसूले-फ़िक़्ह की किताबों में सबसे पहले शब्दकोशीय और तार्किक पहलुओं और मौलिक विषयों पर चर्चा होती है। फिर वे यह बताते हैं कि शरई आदेश क्या है। फिर शरई आदेश के मूलस्रोत कौन-कौन से हैं। फिर वे बताते हैं कि इज्तिहाद (क़ुरआन एवं हदीस के उसूलों पर ग़ौर करके ख़ुद राय क़ायम करना) और तक़लीद (दूसरों की राय का अन्धानुकरण) के मौलिक आदेश क्या हैं। यह चार मौलिक बहसें हैं जो इसी क्रम से विशेषकर उसूले-फ़िक़्ह की इन किताबों में अपनाई गईं जो शाफ़िई फ़ुक़हा या तरीक़ा-ए-मुतकल्लिमीन की शैली के अनुसार लिखी गईं।
जैसा कि आपको इस चर्चा से अनुमान हो गया होगा, इस तरीक़े के अनुसार जो किताबें लिखी गई हैं उनका अंदाज़ एक अनुमानित बहस का है, एक abstract और speculative अंदाज़ का है। जैसे कोई abstract philosophical discussion होता है, इस तरह का अंदाज़ है। इसलिए कि जब उसूल पहले सोचे जाएँगे तो वह जुज़इयात और आम आंशिक समस्याओं से परे होकर सोचे जाएँगे। इसलिए इसमें अनुमान का रंग अवश्य ही पैदा हो जाएगा।
चूँकि इस शैली पर काम करनेवालों में मुतकल्लिमीन ज़्यादा नुमायाँ थे। और मुतकल्लिमीन का स्वभाव ज़्यादा-तर अक़्ली बहसों का था इसलिए उनके यहाँ अनुमानित बहसें ज़्यादा थीं। इसलिए इस शैली को मुतकल्लिमीन ही ने ज़्यादा परवान चढ़ाया। और उनके यहाँ यह शैली ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसमें सबसे पहले शाफ़िई फ़ुक़हा ने, फिर मालिकी फ़ुक़हा ने, फिर हंबली फ़ुक़हा ने, फिर शीया इमामिया ने, फिर फ़िक़्हे-ज़ैदिया के लोगों ने, फिर इबाज़ी फ़िक़्ह के माननेवालों ने इस शैली से काम लिया। बहस का यह सिलसिला इमाम शाफ़िई (रह॰) से लेकर लगभग पाँच सौ वर्ष तक चलता रहा। इन पाँच सौ वर्षों के दौरान इस शैली के अनुसार फ़िक़्ह के सामान्य और विशेष विषयों पर सैंकड़ों किताबें लिखी गईं। उनमें दर्जनों किताबें वे हैं, कम-से-कम पचास के क़रीब वे किताबें हैं जो अत्यन्त रुजहान बनानेवाली साबित हुईं। जिन्होंने उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान को विकसित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से बहुत-सी किताबें ऐसी हैं जो आज भी बहुत महत्व रखती हैं और उसूले-फ़िक़्ह की पूरी संरचना उनके आधार पर क़ायम है।
हनफ़ी फ़ुक़हा का तरीक़ा
दूसरा तरीक़ा ‘तरीक़ा-ए-अहनाफ़’ (हनफ़ी फ़ुक़हा का तरीक़ा) या तरीक़ा-ए-फ़ुक़हा कहलाता है। तरीक़ा-ए-फ़ुक़हा यह है कि पहले आंशिक समस्याओं और आंशिक मतभेदों का जायज़ा लेकर यह देखा जाए कि उनका आधार किन सिद्धान्तों पर है और क्यों अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन ने ये रायें क़ायम कीं। चूँकि इस तरीक़े से सबसे पहले हनफ़ी फ़ुक़हा ने काम लिया, इसलिए इसको तरीक़ा-ए-अहनाफ़ भी कहते हैं और तरीक़ा-ए-फ़ुक़हा भी कहते हैं। तरीक़ा-ए-फ़ुक़हा इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों ने उसूले-फ़िक़्ह पर इस तरीक़े के अनुसार किताबें लिखीं, उन्होंने पहले यह देखा कि दूसरे बड़े फ़ुक़हा ने जो इज्तिहादात किए हैं वे क्या हैं। उदाहरणार्थ इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने जो इज्तिहादात किए हैं वे क्या हैं। इमाम अबू-यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद ने जो इज्तिहादात किए हैं वे क्या हैं। इन इज्तिहादात पर अलग-अलग ग़ौर किया। और थोड़ा-सा ग़ौर करने के बाद उनके ज़ेहन में वह मौलिक सामने सिद्धान्त आ गया जिसके आधार पर अइम्मा मुज्तहिदीन ने यह इज्तिहादात किए थे। उदाहरणार्थ इमाम शाफ़िई (रह॰) के सामने अमुक उसूल था जिसके तहत उन्होंने यह राय दी है। अब अगर इमाम शाफ़िई (रह॰) से दस मसाइल (शरई आदेश) पूछे गए हों, वे सब-के-सब एक ही प्रकार के हों, और उनमें उन्होंने एक ही जैसा जवाब दिया हो तो इसका अनिवार्य अर्थ यह है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के ज़ेहन में एक निर्धारित उसूल था जिसके आधार पर वे इन सब समस्याओं का एक ही अंदाज़ से जवाब दे रहे थे। गोया उनके इज्तिहाद की प्रक्रिया का आधार इन सब समस्याओं में यही उसूल था। फिर जब यह उसूल मिल गया तो इसको और समस्याओं पर भी चस्पाँ करके देखा गया। अगर परिणाम वही निकलता है तो खोजे गए उसूल दुरुस्त हैं। इस तरह से इस शैली के तहत जुज़इयात का अध्ययन करके उनमें से उसूल निकाले गए। ये उसूल जैसे-जैसे जमा होते गए, कला बनती गई और उसूले-फ़िक़्ह का एक नया ढंग सामने आ गया।
इस विषय पर, यानी उसूले-फ़िक़्ह पर, इस शैली के अनुसार भी किताबें लिखी गईं जिनकी संख्या दर्जनों में है। उनमें प्राचीनतम उपलब्ध किताब इमाम अबू-बक्र जस्सास की ‘उसूलुल-जस्सास’ है। इमाम अबू-बक्र जस्सास अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़क़ीह थे। वह पवित्र क़ुरआन के टीकाकार भी थे। उनकी किताब ‘अहकामुल-क़ुरआन’ मशहूर है जो हर जगह मिलती है। दुनिया की हर इस्लामी दर्सगाह में पढ़ाई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने इसका उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित करवाया है। उन्होंने ‘उसूलुल-जस्सास’ के नाम से पहले किताब लिखी। फिर इन सिद्धान्तों को अपनी टीका में बरतकर दिखाया कि इन सिद्धान्तों के आधार पर क़ुरआन से आदेश कैसे निकाले जाते हैं। यह निराली विशेषता इमाम जस्सास ही को प्राप्त है, शेष लोगों में बहुत कम लोगों को यह सम्मान या विशिष्टता प्राप्त है। शेष लोगों ने भी उसूले-फ़िक़्ह पर किताबें लिखी हैं, लेकिन किसी ने इन सिद्धान्तों के आधार पर कोई टीका या हदीस की व्याख्या लिखकर नहीं बताई कि शरीअत के स्पष्ट आदेशों की व्याख्या ऐसे की जाए। इमाम जस्सास ने यह कारनामा भी करके दिखा दिया। अत: ‘उसूलुल-जस्सास’ के रूप में आपके पास थ्योरी भी है और उसका प्रैक्टिकल भी ‘अहकामुल-क़ुरआन’ के रूप में उन्होंने किया हुआ है, जो प्रकाशित पुस्तक के रूप में मौजूद है।
उसूले-फ़िक़्ह पर तीन किताबें इस शैली के अनुसार बहुत नुमायाँ और मशहूर हैं। फ़ख़रुल-इस्लाम बज़दवी नाम के एक बुज़ुर्ग थे, उनकी किताब ‘उसूलुल-बज़दवी’ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे मशहूर बुज़ुर्ग इमाम सरख़्सी थे, जिनका उल्लेख आगे की चर्चा में आएगा। उनकी किताब ‘उसूलुस-सरख़्सी’ के नाम से मशहूर है। ‘उसूलुल-जस्सास’, ‘उसूलुल-बज़दवी’ और ‘उसूलुस-सरख़्सी’, ये तीन किताबें फ़िक़्हे-हनफ़ी के दृष्टिकोण से मौलिक किताबें हैं। गोया पाँचवीं सदी हिजरी तक आते-आते ये दो बड़ी शैलियाँ या दो बड़ी methodologies सफलता के साथ जारी थीं और इस्लामी विद्वानों ने उनमें इतनी समस्याएँ उठाई हैं और इतनी गहराई में उतरकर उन समस्याओं का जायज़ा लिया है कि पश्चिमी उसूले-क़ानून आज 2004 में भी इस दर्जे तक नहीं पहुँचा। वहाँ अब जो समस्याएँ उठाई जा रही हैं उनको मुसलमान फ़ुक़हा एक हज़ार वर्ष पहले बयान कर चुके हैं, उनका जवाब दिया जा चुका है और उनपर किताबें लिखी जा चुकी हैं।
उसूले-फ़िक़्ह के विषय और विस्तृत विवरण
उसूले-फ़िक़्ह के नाम से जो किताबें इन दोनों शैलियों के अनुसार उपलब्ध हैं और उनमें जो कुछ लिखा हुआ है उनकी पूरी सामग्री और विवरणों को पाँच विषयों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसूले-फ़िक़्ह के विवरण पाँच मौलिक अध्यायों में हैं। सबसे पहले इसमें यह बताया जाता है कि जिसको शरई आदेश कहते हैं वह क्या है। शरई आदेश ही की खोज उसूले-फ़िक़्ह का अस्ल उद्देश्य है। उसूले-फ़िक़्ह की सारी एक्सरसाइज़ का एक मात्र उद्देश्य यह है कि शरीअत के आदेश मालूम हो जाएँ। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सवाल ज्ञानपरक और मंतक़ी दृष्टि से यही होना चाहिए कि शरई आदेश, जिसको कहते हैं वह क्या है? उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके आदेश, यह उसूले-फ़िक़्ह का सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है। उसूले-फ़िक़्ह से अपरिचित लोगों को शायद इस विषय की व्यापकता, गहराई और महत्व का पूरा अनुमान न हो। आज की चर्चा में इसकी एक झलक दिखाऊँगा तो आपको पता चलेगा यह कितना सूक्ष्म और संवेदनशील विषय है। बज़ाहिर तो इसकी संवेदनशीलता का शायद हमें इतना आभास न हो, लेकिन एक-एक शरई आदेश पर विद्वानों ने इतनी इतनी मोटी-मोटी किताबें लिखी हैं जो हज़ारों पृष्ठों के कई भागों पर आधारित हैं। शरई आदेशों के बहुत-से पहलुओं में से एक-एक पहलू पर मोटी-मोटी किताबें लिखी गई हैं।
शरई आदेशों के बाद दूसरा विषय यह है कि शरई आदेशों के मूलस्रोत क्या हैं। दो स्रोत तो सबको मालूम हैं यानी पवित्र क़ुरआन और सुन्नत, जो अस्ली और मौलिक स्रोत हैं। लेकिन पवित्र क़ुरआन ने उनके अलावा भी कुछ उपस्रोतों का उल्लेख किया है। पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह बुद्धि का उल्लेख किया है कि अपनी बुद्धि से काम लो। सोचो, चिन्तन-मनन से काम लो। गोया बुद्धि को पवित्र क़ुरआन ने स्वीकार किया है, अत: शरई आदेशों का बुद्धि भी एक स्रोत है। लेकिन बुद्धि कैसे स्रोत है, इसकी सीमाएँ क्या हैं, इससे काम लेने के क्या नियम हैं। इन सब सवालात का जवाब देने की आवश्यकता है जो उलमाए-उसूल ने विस्तार के साथ दिया है। फिर पवित्र क़ुरआन ने ईमानवालों को आदेश दिया है कि मुसलमानों के तरीक़े पर चलो। और जो लोग मुसलमानों के तरीक़े पर नहीं चलते उनको अज़ाबे-आख़िरत (परलोक की यातना) की सूचना दी है। क़ुरआन में कहा गया है— “जो कोई मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता अपनाएगा तो उसको हम जहन्नम में झोंक देंगे।” (क़ुरआन, 4:115) गोया मुसलमानों के तरीक़े पर चलना और मुसलमानों के साथ रहना यह पवित्र क़ुरआन का आदेश है। इससे ‘इजमा’ का समर्थन होता है कि मुसलमानों में ‘इजमा’ के ज़रिये जो आदेश और जो उसूल तय किए गए हैं उनकी पैरवी अनिवार्य है। वरना अल्लाह तआला जहन्नम का वादा न करता। इससे मालूम होता है कि क़ुरआन और सुन्नत ने स्वयं कुछ सिद्धान्तों की निशानदेही की है जो शरीअत के मूलस्रोत हैं। उनमें कुछ पर मतैक्य है और कुछ के बारे में मतभेद भी है।
तीसरा मौलिक विषय जो उसूले-फ़िक़्ह की किताबों में मिलता है, यह वह है जो सबसे पहली बार उसूले-फ़िक़्ह के ज्ञान के ज़रिये क़ानून जगत् में परिचित हुआ। यह विभाग विशेषकर मुसलमानों का प्रदान किया हुआ है। यह वह विभाग है जिसे इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) ‘दलालात’ (अर्थ विज्ञान) के नाम से याद करते हैं। दलालात को आजकल की शब्दावली में आप उसूले-ताबीरे-क़ानून (क़ुरआन की टीका करने का क़ानून) कह सकते हैं। यानी principles of interpretation उसूले-ताबीरे-क़ानून या उसूले-तफ़सीरे-क़ानून। आज तो दुनिया में हर जगह उसूले-ताबीरे-क़ानून के नाम से एक कला मौजूद है जो कॉलिजों, यूनीवर्सिटीयों और लॉ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन पश्चिम में यह कला सौ दो सौ वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं है। दो सौ वर्ष भी मैंने सावधानीपूर्वक कह दिया। पिछले चार पाँच दिनों में interpretation of statues पर मैंने बहुत-सी किताबें देखीं कि यह पता चले कि इस कला में प्राचीनतम किताब कब की है। मेरा अनुमान यह है कि यह कला पश्चिम में ज़्यादा पुरानी नहीं। मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में इस कला पर अंग्रेज़ी भाषा की जो प्राचीनतम किताब मिली वह 1908 ई॰ की है। इससे पहले की भी कोई किताब शायद मौजूद हो, लेकिन मुझे नहीं मिली। इसलिए सावधानी में दो सौ वर्ष कह देता हूँ। यह कला इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसके विपरीत उसूले-फ़िक़्ह ने ज्ञान के इस विभाग से दुनिया को दूसरी सदी हिजरी के अन्त ही में परिचित करा दिया था। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) में दूसरी सदी हिजरी में इसपर बहसें शुरू हो चुकी थीं कि क़ानून की व्याख्या कैसे की जाए। क़ानून की जो लफ़्ज़ियात (शब्दावलियाँ) हैं उनका क़ानून की व्याख्या पर क्या प्रभाव होता है। कलामे-मुफ़रद और कलामे-मुरक्कब के प्रभाव क्या हैं। जुमले की तर्तीब, यानी वाक्य का ढाँचा syntaxt क्या है, उसका क्या अर्थ है, कोई शब्द आगे आए तो उसका अर्थ क्या होगा, पीछे आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, उसके प्रभाव क्या होते हैं। किसी चीज़ को मना करने के बाद जायज़ क़रार दिया जाएगा तो क्या अर्थ होगा। किसी चीज़ का आरम्भ में आदेश दिया जाएगा तो आदेश का अर्थ क्या होगा। ये सारी मौलिक समस्याएँ हैं। इनके विस्तृत विवरण के बिना क़ुरआन और सुन्नत से लाभान्वित होना मुश्किल है।
‘दलालात’ (अर्थ विज्ञान) की बहस पवित्र क़ुरआन और हदीसे-रसूल को समझने के लिए भी अपरिहार्य है और अन्य क़ानूनों की व्याख्या के लिए भी अपरिहार्य है। उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन में सीग़ा-ए-अम्र (आदेशात्मक भाव) बहुत जगह आया है; “नमाज़ क़ायम करो।” इसमें आदेश दिया गया है। “माँ-बाप के साथ उपकार करो”, इसमें भी आदेशात्मक भाव है। “जब एहराम खोल दो तो शिकार करो”, यह भी आदेशात्मक वाक्य है। “जी चाहे तो स्वीकार करो और न चाहे तो स्वीकार न करो”, यह भी आदेशात्माक वाक्य है। “जहन्नम के अज़ाब को चखो और जहन्नम में घुस जाओ।” यह सारे आदेशात्मक वाक्य हैं। क्या इन सबका एक आदेश है? ज़ाहिर है कि नहीं, इन सबका एक आदेश तो नहीं हो सकता। क्या इन सब-के-सब वाक्यों में आनेवाले आदेशात्मक भाव अनिवार्यता के लिए हैं, या कहीं-कहीं आदेशात्मक भाव धमकी और चेतावनी के लिए भी प्रयुक्त होता है? जहन्नमी व्यक्ति से कहा जाएगा कि “चख तू दुनिया में बड़ा सभ्य और प्रतिष्ठित बनता था।” अब यह ‘ज़ुक़’ (चख) आदेशात्मक भाव है। तो कहाँ आदेशात्मक भाव को आदेश के अर्थ में लिया जाएगा, कहाँ उसका अर्थ धमकी का होगा, कहाँ उसका अर्थ किसी बात का औचित्य बताना होगा, इन सब चीज़ों के नियम होने चाहिएँ। इसको किसी की पसंद-नापसंद पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। यह वे उसूल हैं जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘दलालात’ के नाम से तैयार किए हैं।
मैं निस्संकोच यह कह सकता हूँ कि लगभग एक हज़ार वर्ष का अन्तराल ऐसा गुज़रा है कि मुसलमानों के अलावा इस धरती पर कोई क़ौम क़ानून की व्याख्या के सिद्धान्तों के नाम से किसी संकलित और संगठित कला से परिचित नहीं थी। मुसलमान फ़ुक़हा ने दुनिया को यह ज्ञान प्रदान किया। क़ानून की व्याख्या के उसूल तैयार किए और आज इसपर सैंकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों की संख्या में किताबें मौजूद हैं जिनसे पुस्तकालय भरे हुए हैं।
सीरिया से सम्बन्ध रखनेवाले एक समकालीन फ़क़ीह हैं, जिन्होंने उसूले-तफ़सीरे-क़ानून पर एक बड़ी ज्ञानपरक किताब लिखी है। उनका नाम डॉक्टर शैख़ मुहम्मद अदीब सालेह है। उनकी किताब ‘तफ़सीरुन-नुसूस फ़िल-फ़िक़्हिल-इस्लामी’ है यानी ‘फ़िक़्हे-इस्लामी में क़ानून की व्याख्या के सिद्धान्त’। यह किताब दो मोटी जिल्दों में है। इसमें उन्होंने उन तमाम बहसों का सारांश बयान कर दिया है जो फ़ुक़हा ने इमाम शाफ़िई (रह॰), बल्कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने से लेकर आज तक तैयार कीं और संकलित कीं।
‘दलालात’ के बाद चौथा मौलिक विषय है शरीअत के उद्देश्य और शरई क़ानूनों की तत्वदर्शिता। शरीअत के उद्देश्य क्या हैं और इसकी हिक्मत या तत्वदर्शिता क्या है, इस विषय पर एक दिन अलग से चर्चा होगी। जिसमें मैं उन बहसों का सारांश पेश करूँगा जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इस सवाल के जवाब में किए हैं कि शरीअत के आदेशों की तत्वदर्शिता क्या है। अल्लाह तआला तो हमारा मुहताज नहीं है। अगर सारे इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाएँ तो अल्लाह तआला की हुकूमत में एक कण की बढ़ोतरी नहीं होती और अगर सारे इंसान मिलकर गुमराह हो जाएँ तो उसके साम्राज्य में एक कण की कमी नहीं होती। यह शरीअत तो हमारे फ़ायदे के लिए है। इसके आदेश तो हमारी भलाई के लिए हैं।
पवित्र क़ुरआन में शरीअत के आदेशों पर अमल करने की जो हिकमतें और जो लाभ बताए गए हैं उनमें से कुछ की मिसालें मैं दूँगा। हदीसों में भी इस तरह के लाभ बताए गए हैं। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने विशेषकर और क़ुरआन के टीकाकारों और मुहद्दिसीन ने आम तौर से यह बात स्पष्ट की है कि शरीअत में आदेशों के पीछे एक तत्वदर्शिता मौजूद है। कुछ उद्देश्य हैं जो हमारे लाभ के लिए अल्लाह ने रखे हैं। वे उद्देश्य और हिकमतें क्या हैं, इसको लोगों ने तलाश किया है, इसपर किताबें लिखी हैं और इस काम में अपनी जीवनियाँ लगा दी हैं। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का सहयोग (contribution) भी इस मैदान में कम नहीं है। हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामी विद्वानों में हदीस के सबसे बड़े आलिम, बल्कि इल्मे-हदीस और दीन की बारीकियों के ज्ञान में अमीरुल-मोमिनीन कहलाए जा सकते हैं, उनकी मोटी किताब दो भागों में 'हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ है। इस किताब का यही विषय है। उन्होंने अपने आपको इस किताब में हदीसों के अध्ययन तक सीमित रखा है और यह दिखाने की कोशिश की है कि हदीसों में जो आदेश आए हैं उनकी क्या-क्या हिकमतें हैं। उन्होंने पवित्र क़ुरआन, इज्तिहादी मामलात और इजमा वग़ैरा को इस किताब में सामने नहीं रखा। केवल हदीसों को लिया है और उनपर दो मोटी जिल्दों में किताब तैयार की है। यह उसूले-फ़िक़्ह की बहस करनेवाली किताबों में चौथी किताब है।
पाँचवीं किताब इज्तिहाद पर बहस करनेवाली है। चूँकि इज्तिहाद एक महत्वपूर्ण उसूल है और इसके बहुत-से तरीक़े हैं, जिनसे काम लेकर मुस्लिम समाज ने पिछले चौदह सौ सालों में बहुत-से मामलों का समाधान तलाश किया है। इसलिए इज्तिहाद के नियम-क़ायदे और उसूल भी तय-शुदा और निर्धारित होने चाहिएँ। इज्तिहाद का नाम लेकर शरीअत के आदेशों का इनकार बहुत बड़ा अपराध है। इज्तिहाद का नाम लेकर पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के सिद्धान्तों से मुँह मोड़ना बहुत बड़ा दुस्साहस है। अत: इज्तिहाद के ऐसे सर्वसम्मत और निर्धारित उसूल होने चाहिएँ कि जब इज्तिहाद करनेवाला उनसे काम ले तो पवित्र क़ुरआन की बयान की हुई सीमाओं के अन्दर है। शरीअत के उद्देश्यों का पालन करे और शरीअत के स्पष्ट आदेशों में जो मार्गदर्शन दिए गए हैं उनका पूरा पालन करे। इन सीमाओं के अन्दर रहते हुए शरीअत की रौशनी में समस्याओं का समाधान तलाश करे। शरीअत की सीमाओं से निकलकर अपनी निजी इच्छाओं और पसंद-नापसंद के आधार पर कोई समाधान तलाश न करे। यह उसी समय हो सकता है जब इन नियमों का पालन किया जाए। इन नियमों से बहस इस पाँचवीं किताब के तहत होती है।
ये पाँच मौलिक बहसें हैं जो उसूले-फ़िक़्ह की किताबों में बयान होती हैं। इन सब बहसों में से इज्तिहाद और शरीअत के उद्देश्यों पर अलग से चर्चा होगी, इसलिए मैं इसके विस्तार में अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन शेष तीन विषयों पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं।
शरई आदेश क्या है?
सबसे पहला विषय शरई आदेश (हुक्मे-शरई) है कि शरई आदेश क्या है। शरई आदेश अल्लाह तआला का वह सम्बोधन है जो प्रत्यक्ष रूप से पवित्र क़ुरआन में, या अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुबारक ज़बान से सुन्नत के संग्रह में हम तक पहुँचा हो और जो बंदों के कृत्यों और कर्मों की किसी कैफ़ियत या हैसियत से सम्बन्धित हो। अल्लाह के इस सम्बोधन या सन्देश को इस्लामी परिभाषा में ‘हुक्मे-शरई’ कहते हैं। अल्लाह तआला का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बोधन, जो बंदों के कर्मों से सम्बन्धित हो और उसमें बंदों के कर्मों की कैफ़ियत और प्रकार को बयान किया गया हो, शरई आदेश कहलाता है। इस विषय को उलमाए-उसूल ने कलात्मक भाषा और शब्दावलियों में बयान किया है। यह कलात्मक शब्दावलियाँ ज़रा मुश्किल हैं इसलिए उनको मैं छोड़ देता हूँ।
शरई आदेश का मूलस्रोत
अब इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह सवाल उठाया कि शरई आदेश मालूम करने का ज़रिया किया है। क्या केवल वह्य (प्रकाशना) ही शरई आदेश मालूम करने का ज़रिया है या मानव-बुद्धि भी इसका ज़रिया हो सकती है। इस मामले में मुसलमानों में तीन दृष्टिकोण अपनाए गए। एक दृष्टिकोण उन विद्वानों का है जो ‘अशाइरा’ कहलाते हैं। अशाइरा मुसलमान मुतकल्लिमीन का एक गिरोह है जो इमाम अबुलहसन अशअरी के पैरोकार हैं। आपने अगर अल्लामा इक़बाल की ‘बाले-जिब्रील’ पढ़ी हो तो उसमें यह ‘क़तआ’ ज़रूर पढ़ा होगा—
यह नुक्ता मैंने सीखा बुल-हसन से
कि जाँ मरती नहीं मर्गे-बदन से
यह वही अबुल-हसन अशअरी हैं जिनते नाम से अशाइरा जाने जाते हैं। अशाइरा में बड़े-बड़े विद्वान और बड़े मुतकल्लिमीन शामिल थे। हुज्जतुल-इस्लाम इमाम ग़ज़ाली और इमाम राज़ी अशअरी थे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अशअरी किस दर्जे के लोग होते थे। इन लोगों की राय यह है कि बुद्धि के आधार पर शरई आदेश मालूम नहीं किया जा सकता। बुद्धि का सिरे से कोई रोल और कोई भूमिका शरई आदेश मालूम करने में नहीं है।
एक दूसरा दृष्टिकोण था जो अशाइरा से दूसरी इंतिहा पर है। यह ‘मोतज़िला’ का दृष्टिकोण है जो बुद्धि को अपने-आपमें बुराई-भलाई की कसौटी और शरीअत का स्रोत स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि वह्य और बुद्धि दोनों शरीअत के मूल स्रोत हैं और इंसान अपनी बुद्धि से चीज़ों की अच्छाई-बुराई और कर्मों का बुरा-भला होना मालूम कर सकता है। इस राय के समर्थन में मोतज़िला का कहना था कि शरीअत के आने से पहले भी इंसानों को यह मालूम था कि चोरी बुरा काम है, क़त्ल अपराध है, ग़रीब की सहायता करना नेकी है। जब ये चीज़ें बुद्धि के ज़रिये पहले से मालूम थीं तो फिर बुद्धि यह भी बता सकती है कि शरीअत का मंशा यह है कि क़त्ल और चोरी न की जाए। अगर शरीअत में यह आदेश न भी आता तो हमें बुद्धि के आधार पर पहले से पता था कि शरीअत अमुक-अमुक अच्छे कामों को पसंद और अमुक-अमुक बुरे कामों को नापसंद करती है। अत: इन उदाहरणों से पता चला कि बुद्धि भी शरीअत का स्रोत है। यह मोतज़िला का मसलक है, जिससे मुसलमानों के बहुमत ने स्वीकार नहीं किया।
मुसलमानों के बहुमत का दृष्टिकोण यह है कि बुद्धि से किसी चीज़ का अच्छा या बुरा होना तो मालूम हो सकता है, लेकिन मात्र बुद्धि से मालूम की हुई किसी अच्छी चीज़ के करने पर अल्लाह के यहाँ अज्र नहीं है। और मात्र बुद्धि की बताई हुई किसी बुरी चीज़ के करने पर अल्लाह के यहाँ सज़ा भी नहीं है। पारलौकिक सज़ा और जज़ा केवल वह्य के आधार पर हो सकती है, किसी और आधार पर नहीं हो सकती। अब देखें इसमें बुद्धि की भूमिका भी आ गई कि बुद्धि से किसी चीज़ का अच्छा और बुरा होना तो मालूम हो जाएगा। जो चीज़ बुद्धि ने अच्छी बताई है, निश्चय ही वह अल्लाह की शरीअत में भी अच्छी होगी। जिस चीज़ को बुद्धि ने बुरा क़रार दिया है उसकी प्रबल सम्भावना है कि अल्लाह की शरीअत ने भी उसको बुरा क़रार दिया हो। आप ग़ौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि शरीअत के आदेश और निषेध को बुद्धि भी अच्छा या बुरा क़रार देती है। इस तरह अगर शरीअत से भी बुद्धि का समर्थन हो जाए तो बुद्धि के फ़ैसले की पुष्टि हो गई। और अगर शरीअत से बुद्धि के फ़ैसले का समर्थन न हुआ तो आप दोबारा ज़्यादा गहराई में जाकर ग़ौर करें। हो सकता है कि आपसे समझने में ग़लती हो गई हो।
अब चूँकि बुद्धि के फ़ैसले में ग़लती की सम्भावना रहती है इसलिए मात्र अक़्ली फ़ैसले के आधार पर आख़िरत (परलोक) में इनाम और दंड नहीं हो सकता। कारण स्पष्ट है कि जहाँ-जहाँ फ़ैसले में ग़लती की सम्भावना है वहाँ इस सम्भावना के कारण आख़िरत में सवाब (पुण्य) और इक़ाब (दंड) की परिकल्पना क़ायम नहीं की जा सकती। आख़िरत में इनाम और सज़ा केवल शरीअत के मना करने या आदेश देने पर होगी। यह मुसलमानों में से अधिक बहुमत का दृष्टिकोण है। अत: बहुमत ने इस मामले में न अशाइरा के दृष्टिकोण से सहमति जताई और न मोतज़िला के दृष्टिकोण से। बहुमत ने इस दरमियाने दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है कि बुद्धि से अच्छाई-बुराई तो मालूम हो सकती है, लेकिन आख़िरत में प्रतिदान और दंड, या दुनिया में जो हराम या हलाल होना है वह शरीअत के अनुसार होगा। यह बात शरीअत से हटकर तय नहीं हो सकती।
अतः शरई आदेश देने का अधिकार केवल अल्लाह को है, मानव-बुद्धि को नहीं है। الحاکم والمشرع المکلف ھواللہ سبحانہ وتعالیٰ (शासक और विधि निर्माता केवल अल्लाह तआला है) यह वाक्य सब फ़ुक़हा के यहाँ मिलता है। आदेश देनेवाला, शरीअत देनेवाला, शरीअत के आदेशों के पालन में सक्षम बनानेवाला केवल अल्लाह है और कोई नहीं है। बुद्धि शरीअत का स्रोत नहीं है। बुद्धि शरीअत की समझ और व्याख्या में सहायता दे सकती है, लेकिन मात्र बुद्धि शरीअत का मूलस्रोत नहीं हो सकती। यह प्रतिष्ठित फ़ुक़हा के बहुमत का दृष्टिकोण है।
शरई आदेश के प्रकार
शरई आदेश के दो प्रकार हैं। एक कहलाता है ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ और दूसरा कहलाता है ‘हुक्मे-शरई वज़ई’। ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ वह है जिसके परिणामस्वरूप इंसान को किसी चीज़ का सामर्थ्यवान क़रार दिया गया हो या किसी चीज़ के समर्थ होने से मुक्त क़रार दिया गया हो। यानी या तो यह बताया गया हो कि यह काम करना लाज़िमी है, और या यह बताया गया हो कि यह काम नहीं करना है। या यह बताया गया हो कि तुम्हें इस काम के करने या न करने की अनुमति है। इन तीनों में से कोई एक बात बताई गई हो। यह ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ कहलाता है। दूसरा प्रकार होता है ‘हुक्मे-शरई वज़ई’। इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई काम करने का आदेश नहीं दिया जाता न किसी काम के करने से प्रत्यक्ष रूप से रोका जाता है, लेकिन किसी दूसरे काम के करने के लिए जो अपरिहार्य हालात या अपरिहार्य कारण या स्थितियाँ हैं उनकी निशानदेही की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि “लोगों पर अल्लाह का हक़ है कि जिसको वहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य प्राप्त हो, वह उस घर का हज करे” (क़ुरआन, 3:97) इस एक आयत में दोनों आदेश मौजूद हैं। ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ भी है और ‘हुक्मे-शरई वज़ई’ भी है। इसमें ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ यह है कि “लोगों पर यह अल्लाह का हक़ है कि वे उस घर का हज करें।” गोया इस आदेश के ज़रिये मुसलमान हज का सामर्थ्यवान हो गया और उसपर हज करना वाजिब और फ़र्ज़ है। “जो उस तक पहुँचने की सामर्थ्य रखता हो।” यह उन लोगों के लिए है जिनको सामर्थ्य हो और वे वहाँ तक जा सकते हैं। गोया आयत के दूसरे हिस्से में उन हालात को बयान किया गया है जिनमें यह आदेश अनिवार्य होगा। यह ‘हुक्मे-शरई वज़ई’ है। प्रत्यक्ष रूप से सामर्थ्य पर न आप अमल करेंगे, न करने की माँग है। सामर्थ्य कोई अमल करने या न करने की बात नहीं है। लेकिन इस आयत से हज करने या न करने की हालत या कैफ़ियत का पता चल जाता है। इस तरह के आदेशों को ‘हुक्मे-शरई वज़ई’ कहते हैं।
‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ के प्रकार
‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ के कई प्रकार हैं। ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ की एक क़िस्म वह है जिसके तहत एक फ़र्ज़ या कर्म अदा होता है या क़ज़ा होता (छूटता) है। नमाज़ अदा होगी या छूटेगी। रोज़ा अदा होगा या छूटेगा। एक और विभाजन वह है जिसके अनुसार कोई कर्तव्य परम कर्तव्य या वाजिब ‘वाजिबे-मुअय्यन’ होता है या किफ़ाई होता है। एक फ़र्ज़े-ऐन (परम कर्तव्य) है एक फ़र्ज़े-किफ़ाया (वह फ़र्ज़ जिसे कुछ लोग अदा कर लें तो काफ़ी हो जाए और जो कोई भी अदा न करे तो सब गुनहगार होंगे) है। एक वह है जो हर एक पर फ़र्ज़ है दूसरा वह है जो कुछ लोगों पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़े-किफ़ाया फ़र्ज़ तो है, लेकिन कुछ लोगों पर फ़र्ज़ है। वह सब लोगों पर आम तौर पर फ़र्ज़ नहीं होता। यानी एक फ़र्ज़ तो वह होता है जो कुछ लोगों के लिए अनिवार्य है दूसरा फ़र्ज़ वह है जो सब लोगों के लिए अनिवार्य है। यह एक अलग विभाजन है। इसके अलग आदेश हैं।
एक दूसरा विभाजन है ‘वाजिबे-मुज़ीक़’ और ‘वाजिबे-मुवस्सा’। ‘फ़र्ज़े-मुज़ीक़’ (या ‘वाजिबे-मुज़ीक़’) वह फ़र्ज़ है जो अभी या अपने निर्धारित समय पर करना है। वह न एक घंटा आगे हो सकता है न एक घंटा पीछे हो सकता है। जैसे रोज़ा है। आप रोज़ा सुबह होने से पहले एक निर्धारित समय पर ही बंद कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं जी हम तो आठ बजे बंद करेंगे। इसके बंद करने में एक मिनट का भी अन्तर नहीं होगा। और जब खुलना है तो उसी समय खुलेगा। यह नहीं हो सकता कि हम एक घंटा पहले खोल दें या एक घंटा बाद में खोलें। या जैसे हज है। वह भी फ़र्ज़े-मुज़ीक़ है। हज के लिए नौ ज़िल-हिज्जा का दिन मुक़र्रर है। इसमें परिवर्तन का किसी को कोई अधिकार नहीं कि कोई कहे कि नहीं जी नौ को तो बड़ा मुश्किल है, हम ग्यारह को करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हज ज़िल-हिज्जा ही में होगा, नौ तारीख़ ही को होगा। किसी और महीने की किसी और तारीख़ में नहीं हो सकता। यह वह फ़र्ज़ है जो ‘मुज़ीक़’ कहलाता है। जिसका ज़माना और समय निर्धारित है और आगे पीछे नहीं हो सकता।
दूसरी फ़र्ज़े-मुवस्सा’ होता है। इसको अदा करने के लिए समय में गुंजाइश होती है और आप अपनी सुविधानुसार इस गुंजाइश से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरणार्थ ज़ुह्र की नमाज़ है, इसका समय दिन के साढ़े बारह या सवा बारह बजे से शुरू हो जाता है और मतभेदों के अनुसार कई घंटे तक शेष रहता है। आप ज़ुह्र की नमाज़ सवा बारह बजे भी पढ़ सकते हैं, साढ़े बारह बजे भी पढ़ सकते हैं, एक डेढ़ बजे भी पढ़ सकते हैं। आपको अधिकार है। इसी तरह हज को आम तौर पर अदा करने का मामला है। आप इस वर्ष नहीं जा सके तो अगले वर्ष चले जाएँ, इससे अगले वर्ष या इससे भी अगले वर्ष चले जाएँ। आपको इसमें अधिकार है। रोज़ा आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है और वह क़ज़ा हो गया तो क़ज़ा रखना तो ज़रूर है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि रमज़ान के तुरन्त बाद रखें, उससे अगले महीने या किसी और महीने में रखें, आपको अधिकार है। यह वह है जिसको ‘वाजिबे-मुवस्सा’ कहा जाता है और इसमें व्यापकता है कि जब चाहें करें। यह ‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ के उप प्रकार हैं।
‘हुक्मे-शरई तकलीफ़ी’ में फिर उप विभाजन हैं। एक विभाजन के अनुसार कर्म का प्रकार बताया जाता है कि इसकी अनिवार्यता किस दर्जे की है। एक वह है जो निश्चित और अनिवार्य रूप से फ़र्ज़े-ऐन है। हर व्यक्ति को करना है। दूसरा प्रकार वह है जो किफ़ाया है कि कुछ लोग कर लें तो काफ़ी है। कुछ लोग न करें तो भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा।
इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) उसका एक और विभाजन करते हैं। शेष फ़ुक़हा यह विभाजन नहीं करते और उनके यहाँ फ़र्ज़ और वाजिब का एक ही अर्थ है। इमाम शाफ़िई (रह॰), इमाम अहमद (रह॰) और इमाम मालिक (रह॰) के यहाँ अगर यह कहा जाए कि यह वाजिब है या यह फ़र्ज़ है तो दोनों का अर्थ एक ही है। इमाम अबू-हनीफ़ा के नज़दीक फ़र्ज़ का दर्जा ऊँचा है, वाजिब का दर्जा इससे नीचे है। वे यह कहते हैं कि अगर दलीले-क़तई (पुष्ट प्रमाण) से यह साबित हो कि यह फ़र्ज़ है तो वह फ़र्ज़ कहलाएगा, और अगर दलीले-ज़न्नी (अनुमानित प्रमाण) से साबित हो तो वह वाजिब कहलाता है। दलीले-क़तई का इनकार करनेवाला इस्लाम के दायरे से बाहर है और दलीले-ज़न्नी का इनकार करनेवाला इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं होता। इसलिए इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) इस फ़र्ज़ीयत के दो दर्जे क़रार देते हैं। शेष फ़ुक़हा के यहाँ यह अन्तर नहीं है। लेकिन यह मात्र एक इस्तिलाही (पारिभाषिक) चीज़ है। फ़र्ज़ीयत (अनिवार्यता) पर दोनों सहमत हैं और उनका पालन करने को दोनों ज़रूरी समझते हैं।
इसके बाद दर्जा ‘मंदूब’ का आता है जिसको शरीअत ने recommend किया है यानी शरीअत ने इसके करने की सिफ़ारिश की है और इस बात को पसंद किया है कि आप इस कार्य को करें। अलबत्ता उसका करना अनिवार्य नहीं है। ताकीद की गई है कि आप करें तो अच्छा है, न करें तो आपकी मर्ज़ी। मंदूब में भी फिर कुछ उप श्रेणियाँ हैं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) उसके दो दर्जे क़रार देते हैं। एक मंदूब का दर्जा ज़रा ऊँचा है और दूसरे मंदूब का दर्जा ज़रा कम है। जिसे हम ‘सुन्नते-मुअक्कदा’ या ‘सुन्नते-ग़ैर-मुअक्कदा’ कहते हैं। इसके बाद ‘मुबाह’ का दर्जा है कि आप जी चाहे तो करें और जी न चाहे तो न करें। फिर इसी तरह से ‘हराम’ का दर्जा है, जो पूरे तौर पर हराम है। फिर मकरूह यानी नापसंदीदा है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) इसके भी दो दर्जात क़रार देते हैं। ज़्यादा नापसंदीदा और कम नापसंदीदा। वह इसके लिए ‘मकरूहे-तहरीमी’ और ‘मकरूहे-तंज़ीही’ की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं।
ये शरीअत के आदेशों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं जिनमें से हर श्रेणी के आदेश और विस्तृत निर्देश अलग-अलग हैं। एक मुसलमान बचपन से यह सुनता चला आता है कि यह वाजिब है, वह सुन्नत है, यह मुस्तहब है, वह मकरूह है। वह जो कहते हैं कि घर की मुर्ग़ी दाल बराबर होती है, यह कहावत फ़िक़ही दौलत पर भी फ़िट बैठती है। कोई चीज़ अपने पास हो तो उसके महत्व का अनुमान नहीं होता। सच तो यह है कि आदेशों की श्रेणियों का यह विभाजन इतनी मौलिक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया के क़ानून अभी तक इस चीज़ से परिचित तो क्या होते और इसको क्या अपनाते, अभी तक इस धारणा से परिचित भी नहीं हैं। दुनिया के क़ानूनों में दो ही स्थितियाँ होती हैं या तो किसी काम के करने का आदेश होता है कि यह करो, और या किसी काम को करने का निषेध होता है कि इसको मत करो। दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता। यह एक अप्राकृतिक और अवास्तविक विभाजन है। इंसानों के कर्म और गतिविधियों के यही दो प्रकार नहीं हुआ करते। यही वजह है कि इस अवास्तविक विभाजन के कारण कार्यान्वयन के मामले में दुनिया के तमाम क़ानून फ़ेल हो गए। वे चाहते हैं कि एक काम को किया जाए। क़ानून में कोई चीज़ लाज़िम हो और लोग न करें तो सज़ा देनी पड़ती है। सज़ा दें भी तो हल्की-सी बात पर किस-किस को सज़ाएँ देते फिरें। छोटी सज़ा रखें तो शायद लोग सज़ा भुगतें और फिर भी वह काम न करें जो क़ानून के अनुसार अनिवार्य है। यह रोज़ अदालतों में हो रहा है और क़ानून की असफलता साफ़ नज़र आती है। कुछ मामलों को क़ानून रोकना चाहता है। लेकिन उनको अनिवार्य रूप से हराम और ग़ैर-क़ानूनी भी क़रार नहीं देना चाहता। यहाँ क़ानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में नाकाम साबित होता है। उसके सामने सिवाय उस कार्य को निषिद्ध क़रार देने के कोई और रास्ता नहीं होता। इसलिए ग़ैर-क़ानूनी क़रार देकर थोड़ी-सी सज़ा मुक़र्रर कर लेते हैं। इसका परिणाम व्यावहारिक रूप से यह निकलता है कि लोग जुर्माने भरकर अपराध को जारी रखते हैं।
शरीअत ने आरम्भ से इस उलझन का समाधान बता दिया और ये दर्जे पहले दिन से समझा दिए कि हर मामला एक दर्जे का नहीं होगा। कुछ मामलात बहुत अच्छे और अपरिहार्य होंगे जो मुस्लिम समाज में अनिवार्य रूप से होने चाहिएँ वे अनिवार्य और क़ानूनी रूप से अनुपालन योगय समझे जाएँगे। इन मामलात के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। इस तरह कुछ मामलात जो ग़लत और बुरे हैं उनसे इस्लामी समाज को बचाना चाहिए। उनको ‘हराम’ क़रार दिया गया है। इसके हराम होने में कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान भी कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी नापसंदीदा होंगी कुछ हल्की नापसंदीदा होंगी, कुछ कम पसंदीदा होंगी कुछ ज़्यादा पसंदीदा होंगी। सबके आदेश अलग-अलग होंगे। और लोगों को नसीहत की जाएगी कि वह इसको अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें। पसंदीदा कामों को करें और नापसंदीदा कामों से बचें।
कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इस्लाम के शिष्टाचारों में से हैं, और ‘मुस्तहब्बात’ के बिलकुल हल्के दर्जे पर हैं। उनमें से जिन बातों का समर्थन हदीसों से भी होता है उनको ‘सुनने-ज़वाइद’ कहा जाता है। यह ‘मुस्तहब्बात’ में सबसे ऊँचा दर्जा रखते हैं। उदाहरणार्थ सुनने-ज़वाइद में से है कि मस्जिद में जाते समय दायाँ क़दम पहले रखो और निकलते समय बायाँ क़दम पहले निकालो। इन बातों पर अमल करने के लिए क़ानून की ताक़त के बजाय शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रेरणा से काम लिया जाता है। अगर इंसान इन बातों को स्वभाव का हिस्सा बना ले तो वह ख़ुद-ब-ख़ुद इनका अभ्यस्त हो जाएगा और भली-भाँति इनपर अमल करने लगेगा। अगर वह इन बातों को आदत न बनाए तो छोटी-छोटी बातों पर भी अमल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो चीज़ अभी तक दुनिया के क़ानून नहीं समझ सके और जिस मानव स्वभाव और मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रख सके, वह इस्लाम में आरम्भ से मौजूद है, मानव स्वभाव और मनोविज्ञान का ध्यान इस्लाम में पहले दिन से मौजूद है।
चूँकि हमने कभी इसका अनुमान नहीं किया कि यह कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम समझते हैं कि एक आम-सी बात है। लेकिन दुनिया की दूसरी क़ानून व्यवस्थाओं में क्या मुश्किलें और समस्याएँ पेश आती हैं वे समस्याएँ हमारे सामने हों तो फिर अनुमान होगा कि यह कितनी बड़ी चीज़ है और शरीअत ने इस मसले को किस आसानी से हल कर दिया है।
यह शरई आदेशों के विषयों का एक अत्यन्त सरसरी-सा सारांश है। ‘हुक्मे-शरई वज़ई’ का विवरण चूँकि बहुत कलात्मक है इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। कारण क्या है, रुकावट क्या है, शर्त किया है। कभी-कभी कारण और शर्त एक जगह जमा हो जाते हैं तो वहाँ किसी हद तक कारण है, किसी हद तक शर्त है। यह बड़ी गहरी बहसें हैं जिनको अच्छी तरह समझने के लिए लम्बा समय दरकार है। यों भी उसूले-फ़िक़्ह के एक आरम्भिक परिचय में सम्भवत: इनकी आवश्यकता नहीं।
शरीअत के मूल स्रोत
एक और दूसरा मौलिक विषय या मैदान शरीअत के मूल स्रोतों का है कि शरीअत के मूल स्रोत कौन-कौन से हैं। इस सिलसिले में पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के स्रोत होने पर तो कोई दोरायें नहीं हो सकतीं। सबसे पहले और मौलिक स्रोत तो यही दो हैं। और अगर यह कहा जाए कि शरीअत और इस्लामी क़ानून का मूल स्रोत यही दो हैं, तो यह ग़लत नहीं होगा। इन दोनों का आधार चूँकि अल्लाह की वह्य पर है इसलिए यह कहना दुरुस्त है कि इस्लामी क़ानून और शरीअत का अल्लाह की वह्य के अलावा कोई और स्रोत नहीं है। यानी अस्ल और अपने-आपमें अगर कोई स्रोत है तो वह केवल और केवल पवित्र क़ुरआन और सुन्नत हैं। शेष चीज़ें अगर स्रोत हैं तो पहले स्रोत के प्रमाण के आधार पर उनका स्रोत होना साबित होता है। दूसरे शब्दों में केवल क़ुरआन और सुन्नत के बताने से पता चला कि कुछ और चीज़ें भी स्रोत हैं। अगर क़ुरआन और सुन्नत ने उनको स्वीकार न क्या होता तो वे स्रोत नहीं थे। चूँकि पवित्र क़ुरआन ने मानव-बुद्धि की भूमिका को स्वीकार किया है, इसलिए फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन और विकास में बुद्धि की भी एक भूमिका है। पवित्र क़ुरआन ने मुसलमानों के सामूहिक रवैये की पैरवी का आदेश दिया तो पता चला कि मुसलमानों का सामूहिक फ़ैसला भी एक महत्व रखता है। इसी तरह से शेष चीज़ें हैं जिनमें से हर एक की सनद (प्रमाण) पवित्र क़ुरआन में मौजूद है। जो शेष स्रोत हैं उनमें ज़्यादा नुमायाँ इजमा, क़ियास, इस्तेहसान मसालेहे-मुर्सला, उर्फ़ और इस्तिसहाब शामिल हैं।
इजमा : क़ानून के स्रोत के रूप में
‘इजमा’ से मुराद यह है कि किसी शरई या फ़िक़ही मसले पर मुस्लिम समाज के तमाम मुज्तहिदीन सर्वसम्मत रूप से फ़ैसला कर लें जिसे मुस्लिम समाज स्वीकार करले, वह ‘इजमा’ है। मुसलमानों में किसी भी शरई या फ़िक़ही मसले पर उम्मत के तमाम मुज्तहिदीन का वह सर्वसम्मत फ़ैसला, जिसपर मुस्लिम समाज कार्यान्वयन शुरू कर दे, वह इजमा कहलाता है। क़ुरआन और सुन्नत के बाद यह शरीअत का सबसे बड़ा और एक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने बहुत-से मामलों पर सर्वसहमति से फ़ैसला किया। वह फ़ैसला इसी तरह शरीअत का स्रोत है जिस तरह सुन्नत शरीअत का स्रोत है। उदाहरणार्थ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने फ़ैसला किया कि अगर कोई व्यक्ति ज़कात का इनकार करता है तो उसको इसी तरह समझा जाएगा जैसे कोई व्यक्ति नमाज़ का इनकार करता हो। और जो नमाज़ का इनकार करता है वह इस्लाम के दायरे से बाहर है, अत: ज़कात के इनकारी को भी इस्लाम के दायरे से निकला हुआ समझा जाएगा। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नेतृत्व में इन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद किया जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था। शुरू में कुछ सहाबा को यह समझने में संकोच हुआ कि नमाज़ और ज़कात को एक सतह पर कैसे रखा जाए और किसी एक आंशिक आदेश के न मानने को पूरी शरीअत के इनकार के बराबर कैसे माना जाए, लेकिन हज़रत सिद्दीक़े-अकबर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़सम खाकर फ़रमाया कि “क़सम ख़ुदा की, मैं नमाज़ और ज़कात के दरमियान अन्तर नहीं करूँगा और जिसने यह अन्तर किया मैं उसके ख़िलाफ़ जंग करूँगा, यहाँ तक कि मेरी जान इसमें चली जाए।” फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने हमारा सीना भी इस चीज़ के लिए खोल दिया (अर्थात् हम इस बात पर सन्तुष्ट हो गए) जिस चीज़ के लिए हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का सीना खोला था।” बाद में सहाबा फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआला सिद्दीक़े-अकबर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को उत्तम प्रतिदान दे कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता बंद कर दिया कि अगर वे इसको बंद न करते तो आज लोग एक-एक करके इस्लाम के स्तंभों और शरीअत के आदेशों का इनकार करते जाते और आख़िर में शरीअत की हर चीज़ का इनकार हो जाता। यह प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इजमा का सबसे बड़ा उदाहरण है।
इजमा पर बड़ी लम्बी और विस्तृत बहसें की गई हैं। लेकिन आप मूल रूप से दो चीज़ें अच्छी तरह समझ लें। इजमा से मुराद यह है कि किसी नए पेश आनेवाले फ़िक़ही और शरई प्रकार के मामले पर इस्लामी फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन विस्तारपूर्वक स्वतंत्र रूप से यानी किसी हुकूमती, सरकारी या बाह्य प्रभाव के बिना मात्र तर्कों की रौशनी में चिन्तन-मनन करें और क़ुरआन और सुन्नत के तर्कों की रौशनी में उसका समाधान तलाश करें। फिर उनके आपस के विचार-विमर्श से जब वह सर्वसम्मत रूप से किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच जाएँ तो वह सर्वसम्मत निष्कर्ष और फ़ैसला इजमा कहलाएगा। इसके लिए न किसी समय की क़ैद है और न कोई लगी बँधी कार्य-विधि है। इजमा का रूप यह नहीं होता कि कुछ लोग जलसा या सभा का आयोजन करें और कुछ उलमा जमा होकर कोई प्रस्ताव पारित कर लें। इजमा इस तरह नहीं होता। महत्वपूर्ण और संवेदनशील फ़िक़ही और शरई मामलों के फ़ैसले यों प्रस्तावों और सभाओं से नहीं हुआ करते। इन मामलों पर तो विद्वान लम्बे समय तक विचार करते हैं, अपने दृष्टिकोण को दूसरों के सामने पेश करते रहते हैं, तर्कों और जवाबी तर्कों का ठंडे दिल से लम्बे समय तक आदान-प्रदान होता रहता है, फिर अन्ततः सब एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। कभी-कभी इस सर्वसहमति में कुछ महीने लगते हैं और कभी-कभी कई वर्ष लग जाते हैं और कभी-कभी सदियाँ भी लग सकती हैं। जितनी महत्वपूर्ण समस्या होगी उतने ही विस्तार और सूक्ष्मता से लोग विचार करेंगे। फिर अन्ततः मुस्लिम समाज का एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण क़ायम हो जाएगा और सब लोग उसको अपना लेंगे।
कुछ लोगों का ख़याल है कि इजमा को संस्थागत रूप देना चाहिए, यानी इजमा को पश्चिमी अंदाज़ की institutionalization के अधीन किया जाए। इससे उन लोगों का मतलब यह होता है कि अपनी पसंद या अपने वर्ग के परिचय के विद्वानों का कोई अधिवेशन बुलाएँ। उसमें कुछ लोग ज़ोरदार भाषण दें। दो-तीन लोग ज़ोरदार तरीक़े से अपने विचार व्यक्त करें। फिर एक साहब प्रस्ताव पेश करें और सब लोग हाथ उठाकर उसका समर्थन कर दें। याद रखिए, इस तरह के सामयिक और जज़बाती माहौल में किए जानेवाले फ़ैसलों से इजमा क़ायम नहीं हुआ करता। इस तरह के जज़बाती फ़ैसले तो रोज़ होते हैं और रोज़ बदलते भी हैं। आज एक फ़ैसला होता है तो कल ही उसके ख़िलाफ़ रायें आनी शुरू हो जाती हैं। एक कहता है कि जनाब मैंने तो अमुक साहब की ख़ातिर हाथ उठा दिया था। दूसरा कहता है कि जी अमुक का भाषण बड़ा ज़बरदस्त था, मैंने तो इसके बहाव में बहकर समर्थन कर दिया था। समझ लीजिए कि शरीअत के मामलात इस तरह के हंगामी और वक़्ती माहौल में मात्र ज़ोरदार भाषणों और कुछ व्यक्तियों के निजी प्रभावों या व्यक्तिगत आकर्षण की बुनियादों पर तय नहीं होते। इन मामलों का फ़ैसला लम्बे विचार-विमर्श के बाद होता है। सम्बन्धित मामलों पर विस्तार से सोचा जाता है। दर्सगाहों में बहसें होती हैं। शोधकर्ता अपने शोध-कार्य के निष्कर्षों और तर्कों से दूसरे शोधकर्ताओं को अवगत करते हैं, और यों लोगों के वर्षों सोचते रहने, तर्क बयान करने और क़ुरआन और सुन्नत के एक-एक शब्द पर ग़ौर करते रहने के बाद अन्ततः एक सर्वसम्मत राय बनती है। जितना महत्वपूर्ण मसला होगा उसके तय होने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसकी मिसालें अनगिनत हैं और समय कम है। इसलिए मिसालें देने से परहेज़ करता हूँ, आप चाहें तो इजमा पर संकलित होनेवाली किताबें देख लें। उदाहरणार्थ इब्ने-हज़्म की ‘मरातिबुल-इजमा’ वग़ैरा।
कुछ लोगों की ये बातें आपने सुनी होंगी कि मुसलमानों के मौलवी तो पहले हर चीज़ को नाजाइज़ कहते हैं बाद में जायज़ क़रार दे देते हैं। यह बात इजमा के तरीक़े की समझ न होने की वजह से कही जाती है। बात यह है कि जब कोई नई चीज़ पेश आएगी तो उसके बारे में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) और शरीअत के विशेषज्ञ ग़ौर करेंगे। कुछ लोग शायद शुरू-शुरू में यह राय क़ायम करें कि यह नाजाइज़ है। कुछ लोग आरम्भ ही से यह राय क़ायम करेंगे कि यह चीज़ जायज़ है। लेकिन इन दोनों के तर्क एक-दूसरे के सामने आते-जाते रहेंगे। अन्ततः तर्कों और रायों के लम्बे आदान-प्रदान के बाद विद्वान एक-दूसरे की रायों और लोग एक-दूसरे के तर्कों से सहमति जताएँगे। कुछ लोग फिर भी मतभेद करेंगे। इसपर चर्चा और परिचर्चा वर्ष दो वर्ष, दस वर्ष या इससे भी ज़्यादा समय तक जारी रहेगी और अन्ततः सब एक राय पर सहमत हो जाएँगे। उस समय सब सहमति से उस राय को मान लेंगे और हर मुसलमान उस राय से सहमत होकर उसपर अमल करना शुरू कर देगा। इस सर्वसम्मत राय को ‘इजमा’ कहते हैं। इजमा का सम्बन्ध किसी अधिवेशन, बैठक या प्रस्ताव से नहीं होता। जब इजमा आयोजित हो जाता है तो उम्मत को यह मालूम हो जाता है कि इस बात पर इजमा हो चुका है। यह कहना कि इजमा का पता कैसे चलेगा, इजमा की हक़ीक़त को न जाने की वजह से है। इजमा का कोई गज़ेट नोटिफ़िकेशन नहीं होता कि गज़ट में आ गया और नोटिफ़िकेशन हो गया। इजमा का पता हर मुसलमान को हो जाता है, इसलिए कि इजमा-ए-उम्मत में उम्मत की सामूहिक समझ और सामूहिक हिक्मत (तत्वदर्शिता) शामिल होती है। उदाहरणार्थ हर मुसलमान जानता है कि ख़त्मे-नुबूवत (मुहम्मद सल्ल॰ को आख़िरी रसूल मानना) का इनकार करनेवाला मुसलमान नहीं रहता है। क़ुरआन में स्पष्ट रूप से इन शब्दों में यह विषय कहीं नहीं आया कि जो ख़त्मे-नुबूवत को नहीं मानता वह मुसलमान नहीं है, लेकिन हर मुसलमान को मालूम है कि ख़त्मे-नुबूवत का इनकार करनेवाला इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। इसलिए कि इसपर इजमा है और हर पढ़ा-लिखा मुसलमान इस बात को जानता है।
इज्तिहाद और क़ियास
फ़िक़्हे-इस्लामी का चौथा स्रोत ‘इज्तिहाद’ और ‘क़ियास’ है। जिस चीज़ को क़ियास कहते हैं वह इज्तिहाद ही का एक प्रकार है। शरीअत का चौथा स्रोत तो वास्तव में इज्तिहाद है। लेकिन चूँकि क़ियास इज्तिहाद की सबसे बड़ा प्रकार, बल्कि सबसे बड़ा mode है इसलिए बहुत-से लेखक इज्तिहाद की जगह क़ियास को चौथा मूल स्रोत क़रार देते हैं।
इज्तिहाद यों तो चौथे नम्बर पर बयान किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक क्रम की दृष्टि से इसका नम्बर तीसरा होना चाहिए। यह वह स्रोत है जिसकी स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मंज़ूरी दी थी। पवित्र क़ुरआन में अप्रत्यक्ष रूप से इज्तिहाद की तरफ़ इशारे हैं और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति प्रदान की। हज़रत मआज़-बिन-जबल से उल्लिखित मशहूर हदीस आपने सुनी होगी। जो हदीसे-मआज़ के नाम से मशहूर है। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बयान कर देता हूँ।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से लगभग सात आठ माह पहले हज़रत मआज़ को यमन का क़ाज़ी बना कर भेजा था। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत मआज़ को यमन जाने के लिए रुख़स्त कर रहे थे तो उनकी आँखों में आँसू थे। नबी (सल्ल॰) हज़रत मआज़ से बहुत मुहब्बत करते थे। इस मौक़े पर उन्होंने हज़रत मआज़ से कहा कि “ऐ मआज़ मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ।” इसके बाद नबी (सल्ल॰) ने कहा कि “ऐ मआज़ शायद उसके बाद तुम मुझे न देख सको।” यह कहते समय नबी (सल्ल॰) की आँखों में आँसू आ गए और ज़ाहिर है कि हज़रत मआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। इस मौक़े पर नबी (सल्ल॰) ने हज़रत मआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पूछा कि तुम मामलात का फ़ैसला कैसे करोगे? उन्होंने जवाब दिया कि “मैं अल्लाह की किताब के अनुसार फ़ैसला करूँगा।” फिर नबी (सल्ल॰) ने पूछा कि “अगर अल्लाह की किताब में कोई समाधान न मिले तो क्या करोगे?” उन्होंने कहा कि “अल्लाह के रसूल की सुन्नत के अनुसार फ़ैसला करूँगा।” नबी (सल्ल॰) ने कहा, “अगर उसमें भी न मिला तो क्या करोगे?” हज़रत मआज़ ने जवाब दिया कि “मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और कोई कसर उठा न रखूँगा।” यह सुनकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आपके कन्धे पर थपकी दी और कहा कि “अल्लाह तआला की तारीफ़ और शुक्र है कि उसने अल्लाह के रसूल के एलची को उस रास्ते की हिदायत दी जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की ख़ुशी है।” गोया इज्तिहाद को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आदेश के मालूम करने का एक जायज़ तरीक़ा क़रार दिया और पसंद किया।
क़ियास : क़ानून के स्रोत के रूप में
इज्तिहाद के बहुत-से तरीक़े और ढंग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित तरीक़ा ‘क़ियास’ है। ‘क़ियास’ चूँकि इज्तिहाद का सबसे महत्वपूर्ण तरीक़ा है और अभी तक जितना इज्तिहाद हुआ है उसका नव्वे-पचानवे प्रतिशत ‘क़ियास’ ही के ज़रिये हुआ है। इसलिए बहुत-से फ़ुक़हा इज्तिहाद के बजाय ‘क़ियास’ ही की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं, जबकि बहुत-से दूसरे फ़ुक़हा इज्तिहाद की शब्दावली के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मूल स्रोत इज्तिहाद है और ‘क़ियास’ उसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क़िस्म है। ‘क़ियास’ का सीधा-सादा अर्थ शब्दकोशीय दृष्टि से यह है कि किसी अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु के सामने रखकर उसकी रौशनी में इसका फ़ैसला करना। जब महिलाएँ कपड़ा ख़रीदकर लाती हैं तो पहले से सिला हुआ जोड़ा सामने रखकर उसके अनुसार नापकर वे कपड़ा सी लेती हैं। इस नापने को अरबी शब्दकोश में ‘क़ियास’ कहते हैं। ‘मिक़्यासुल-हरारत’ की शब्दावली आपने सुनी होगी यानी गर्मी नापने का पैमाना— थर्मामीटर। तो ‘क़ियास’ का अर्थ नापना है। लेकिन ज्ञानपरक शब्दावली में किसी अज्ञात वस्तु का आदेश ज्ञात वस्तु से नापकर या उसकी रौशनी में अनुमान करके मालूम करना, उसको ‘क़ियास’ कहते हैं।
शरीअत और फ़ुक़हा की शब्दावली में ‘क़ियास’ से मुराद यह है कि अस्ल आदेश में पाए जानेवाले कारण को दूसरे नए आदेश पर चस्पाँ करना। इसलिए कि दोनों समान मालूम होते हैं। यह परिभाषा इमाम ग़ज़ाली ने अपनी किताब 'शिफ़ाउल-अलील’ में की है। उनके शब्द हैं “वह वास्तविक आदेश जो आपको पहले से मालूम है, उसके कारण और वजह को नए आनेवाले आदेश पर चस्पाँ करना और इसका आदेश वहाँ समझना।” क्योंकि कारण में दोनों समान हैं, इसको ‘क़ियास’ कहते हैं।
उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन में शराब का निषेध बयान किया गया है और आदेश दिया गया है कि इससे बचो, “ये शराब और जुआ और देवस्थान और पाँसे तो गंदे शैतानी काम हैं। अतः तुम इनसे अलग रहो।” (क़ुरआन, 5:90) इस आयत के अनुसार शराब हराम क़रार दी गई। अब शराब क्यों हराम क़रार दी गई है, इसके हराम होने की वजह क्या है। अगर यह वजह मालूम हो जाए तो दूसरी कई चीज़ों की हुर्मत (निषेध) या कारण का फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। उदाहरणार्थ किसी ने मसला पूछा कि अफ़ीम खाऊँ या नहीं। अब अफ़ीम के वैध या अवैध होने का ज़िक्र स्पष्ट रूप से न क़ुरआन में आया है न हदीस में। अरब में यह चीज़ होती ही नहीं थी। न अरब लोग अफ़ीमी होते थे। यह चीज़ तो ईरानियों में पाई जाती थी। जब ईरानी मुसलमान हुए तो लोगों ने देखा कि उनमें अफ़ीम खानेवाले बहुत लोग पाए जाते हैं। अब फ़ुक़हा के सामने यह मसला आया तो उन्होंने देखा कि शराब के निषेध का जो कारण है, जिसको अंग्रेज़ी क़ानून में ratio decidandi कहते हैं, जिसके आधार पर शराब हराम क़रार दी गई है वह नशा है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। शराब को सामने रखें तो इसमें बहुत-से गुण नज़र आते हैं। तो इसमें एक गुण यह है कि वह नशा लाती है। एक गुण यह है कि उदाहरणार्थ सुर्ख़-रंग की है या ठंडी है या बदबूदार है। ये सारे उसके गुण हैं। उनमें से ज़ाहिर है कि न सुर्ख़ होना हराम होने का कारण है, न ठंडा होना न बदबूदार होना। यह गुण तो और जायज़ चीज़ों में भी पाए जाते हैं। जो गुण शेष जायज़ चीज़ों में नहीं पाए जाते वह शराब का नशा-आवर होना है। अत: साबित हुआ कि शराब सिर्फ़ नशा-आवर होने की वजह से हराम है। अब चूँकि अफ़ीम भी नशा-आवर है इसलिए अफ़ीम को भी नाजाइज़ समझा जाएगा। गोया नशा-आवर होना वह कारण है जो इन दोनों के दरमियान समान रूप से पाया जाता है। इस प्रक्रिया को ‘क़ियास’ कहते हैं। ‘क़ियास’ उसूले-फ़िक़्ह का सबसे मुश्किल विषय है और उसूले-फ़िक़्ह में इससे ज़्यादा जटिल और पेचीदा विषय कोई और नहीं है।
‘क़ियास’ से सम्बन्धित तमाम ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख इस संक्षिप्त चर्चा में तो सम्भव नहीं है, अलबत्ता कुछ मौलिक बातें बयान करने पर बस करता हूँ जिससे यह अनुमान ज़रूर हो जाएगा कि उलमाए उसूल ने ‘क़ियास’ को किस गहराई से देखा और समझा, किस तार्किक और बौद्धिक ढंग से संकलित किया और इससे फ़िक़ही आदेशों को systematic बनाने में किस तरह काम लिया। यहाँ यह बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि उलमाए-उसूल का ‘क़ियास’ यूनानियों के ‘क़ियास’ से भिन्न चीज़ है। यह मात्र संयोग है कि दोनों के लिए ‘क़ियास’ ही की शब्दावली प्रचलित हो गई। उलमाए-उसूल के यहाँ ‘क़ियास’ की परिकल्पना प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात का अध्ययन करने से आई। फिर ताबिईन के दौर में ‘क़ियास’ की शब्दावली प्रस्तावित हुई और ‘क़ियास’ के ज़रूरी आदेश और नियम संकलित हुए। उस समय यूनानियों की तार्किकता का मुस्लिम जगत् में दूर-दूर भी कहीं पता न था। यूनानियों के ज्ञान-विज्ञान विशेषकर तार्किकता की किताबों के अनुवाद तो कहीं जाकर चौथी और पाँचवीं शताब्दी में शुरू हुए, जब उलमाए-उसूल ‘क़ियास’ पर न केवल हज़ारों पृष्ठों पर सम्मिलित लेख संकलित कर चुके थे, बल्कि ‘क़ियास’ के तमाम ज़रूरी नियम एवं आदेश, शर्तें और कार्य-विधि भी विस्तार से तैयार कर चुके थे और अनुमान से काम लेकर हज़ारों नहीं लाखों फ़िक़ही जुज़इयात (आंशिक मामलों) का संकलन भी कर चुके थे। ऐसा मालूम होता है कि जब मुअल्लिम सानी फ़ाराबी के दौर में (चौथी सदी हिजरी में) तार्किकता की किताबों के अनुवाद और संपादन का अभियान ज़ोर-शोर से चल रहा था, उस समय यूनानियों के सिलोजिस्म (syllogism) के लिए उनको ‘क़ियास’ की बनी-बनाई शब्दावली उलमाए-उसूल के यहाँ से मिल गई और मात्र आंशिक अनुकूलता के आधार पर उन्होंने अपने सिलोजिस्म के लिए यही शब्दावली अपना ली।
इस संक्षिप्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उलमाए-उसूल का ‘क़ियास’ यूनानियों के ‘क़ियास’ से भिन्न चीज़ है। यह यूनानी तार्किकता के आयात से बहुत पहले से मुस्लिम जगत् के ज्ञानपरक क्षेत्रों में जानी-पहचानी चीज़ थी। अरबी में तो दोनों के लिए ‘क़ियास’ ही की शब्दावली प्रयुक्त होती है। अलबत्ता अंग्रेज़ी में फ़िक़ही और उसूली अनुमान के लिए anological reasoning और यूनानी अनुमान के लिए syllogism की शब्दावली प्रचलित है।
उलमाए-उसूल ‘क़ियास’ के चार स्तम्भ या मूल तत्व क़रार देते हैं—
- अस्ल (मूल)
- फ़रअ (शाखाएँ)
- हुक्म (आदेश)
- इल्लत (कारण)
‘अस्ल’ से मुराद शरीअत का वह आदेश है जो पहले से मालूम और मौजूद हो और जिसके आधार पर नए मामले का आदेश मालूम किया जाना अभीष्ट हो। ऊपरवाले उदाहरण में शराब का हराम (निषिद्ध) होना अस्ल आदेश है। ‘फ़रअ’ से मुराद वह नई पेश आनेवाली स्थिति है जिसका आदेश अभी मालूम नहीं है और ‘क़ियास’ के ज़रिये मालूम किया जाना अभीष्ट है। इस उदाहरण में अफ़ीम की हैसियत ‘फ़रअ’ की है। आदेश से मुराद हुक्मे-शरई वज़ई का वह विभाजन है जिसमें कर्मों की पाँच या सात स्थितियाँ (फ़ुक़हा के मतभेदों के अनुसार) बताई जाती हैं, यानी फ़र्ज़, वाजिब, मंदूब, मुबाह, मकरूह और हराम।
‘इल्लत’ की बहस
‘इल्लत’ से मुराद वह वजह या गुण है जो ‘अस्ल’ और ‘फ़रअ’ दोनों में समान हो और जिसके आधार पर ‘अस्ल’ का आदेश ‘फ़रअ’ पर चस्पाँ किया जाता हो। उक्त उदाहरण में नशा-आवर होना ‘इल्लत’ है।
‘क़ियास’ की बहसों में सबसे मुश्किल बहस इल्लत ही की है। किसी आदेश की इल्लत मालूम करने के लिए चार तरीक़े उलमाए-उसूल प्रयुक्त करते हैं। इन तरीक़ों को ‘मसालिकुल-इल्लत’ भी कहा जाता है। ये चार तरीक़े निम्नलिखित हैं—
- नस्से-शरई
- ईमा
- इजमा
- तुर्क़े-अक़लीया
जहाँ तक नस्से-शरई का सम्बन्ध है यह इल्लत की खोज का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीक़ा है। पवित्र क़ुरआन और हदीसों में बहुत-से आदेशों की इल्लतें उन आदेशों के साथ ही बता दी गई हैं जिनसे शरई आदेश का आधार आसानी से मालूम हो जाता है। उदाहरण के रूप में सूरा हश्र में जहाँ यह बताया गया है कि ‘फ़ै’ के अमवाल को यतीमों, मिस्कीनों और बे-घर मुसाफ़िरों के लिए रखा जाए, वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आदेश इसलिए दिया जा रहा है कि दौलत की व्यापक रूप से गर्दिश को निश्चित बनाया जाए और दौलत के संकेन्द्रण का रास्ता बंद किया जाए। इस इल्लत (कारण) के देखते हुए हर वह काम नाजाइज़ और शरीअत के ख़िलाफ़ क़रार पाएगा जो दौलत की गर्दिश को कृत्रिम तरीक़े से रोकता हो और जिसके परिणामस्वरूप दौलत एक वर्ग में संकेन्द्रित होती चली जाए।
ऊपर पवित्र क़ुरआन की एक और आयत का ज़िक्र किया जा चुका है जिसमें कुछ निर्धारित समयों के अलावा निजता के आदेशों में नर्मी की अनुमति देते हुए कहा गया है “वे तुम्हारे पास अधिक चक्कर लगाते हैं। तुम्हारे ही कुछ अंश परस्पर कुछ अंशों के पास आकर मिलते हैं।” (क़ुरआन, 24:58) यानी यह नर्मी इसलिए है कि तुमको बहुत अधिक एक-दूसरे के पास आने की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब इस इल्लत के आधार पर बहुत-से नए मामलों का फ़ैसला किया जा सकता है। ऐसे नए हालात में जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के पास आने जाने की आवश्यकता पड़ती हो, इस इल्लत के आधार पर फ़ैसला किया जाएगा और शरीअत की सीमाओं के अन्दर कुछ आदेशों में नर्मी की जा सकेगी।
इल्लत की खोज का दूसरा तरीक़ा ‘ईमा’ कहलाता है। ईमा का शाब्दिक अर्थ है ‘इशारा’ या ‘रम्ज़’। लेकिन यहाँ मुराद यह है कि सन्दर्भ और अन्य संकेतों से इल्लत स्पष्ट होती हो। इल्लत का ज़िक्र नस्से-शरई में स्पष्ट रूप से तो न हो, लेकिन इबारत में ऐसे स्पष्ट इशारे मौजूद हों जिनके आधार पर इल्लत का निर्धारण किया जा सके। उदाहरण के रूप में एक जगह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सवाल किया गया कि क्या ताज़ा खजूर (रत्ब) की बिक्री ख़ुश्क खजूर (छुआरे) के बदले में कमी-बेशी के साथ जायज़ है? इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सवाल किया कि क्या ताज़ा खजूर (रत्ब) का वज़न सूखने के बाद कम हो जाता है? सहाबा ने बताया कि जी हाँ, इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कमी-बेशी के साथ ताज़ा और ख़ुश्क खजूर के आपसी तबादले को नाजाइज़ क़रार दिया।
इस घटना में स्पष्ट रूप से तो किसी इल्लत का ज़िक्र नहीं है। लेकिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सवाल में इस बात का साफ़ और स्पष्ट इशारा मौजूद है कि चूँकि रत्ब के वज़न में ख़ुश्क होने के बाद कमी आ जाती है इसलिए कमी-बेशी के साथ उसकी बिक्री दुरुस्त नहीं। यहाँ वज़न की कमी का इल्लत होना सन्दर्भ से स्पष्ट हो जाता है। इल्लत की खोज और निर्धारण का तीसरा तरीक़ा ‘इजमा’ है। कभी-कभी एक ख़ास ‘नस्स’ (स्पष्ट आदेश) में एक ख़ास हालत में किसी कार्य से मना किया गया होता है। बज़ाहिर वह हालत स्वयं इल्लत बनने के क़ाबिल नहीं होती, लेकिन ज़रा-सा ग़ौर करने से वे सम्भावित मामले सामने आ जाते हैं जो इस आदेश की अस्ल इल्लत हो सकते हैं। इन मामलों में कौन-सा मामला सचमुच इल्लत है, इसका निर्धारण फ़ुक़हा के मतैक्य से ही होता है। उदाहरण के रूप में एक हदीस में कहा गया है “क़ाज़ी ग़ुस्से की हालत में फ़ैसला न करे।” बज़ाहिर ग़ुस्से का होना इस निषेध की इल्लत नहीं है। फ़ुक़हा ने ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि अस्ल इल्लत क़ाज़ी के ज़ेहन और ध्यान का बिखराव है जो ग़ुस्से की हालत में अक्सर हो जाया करता है। अब इस इल्लत के आधार पर मानसिक बिखराव और ध्यान केन्द्रित न होने की हालत में हर ऐसा काम करना नापसंदीदा होगा जिससे दूसरे का हक़ प्रभावित होता हो।
‘तुर्क़े-अक़्लिया’ से मुराद वे तरीक़े हैं जिनमें बौद्धिक तर्कों के द्वारा इल्लत की खोज लगाई जाए। यह इल्लत की बहसों में सबसे मुश्किल और जटिल विषय है। बौद्धिक तर्कों से इल्लत के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण और जाना-माना तरीक़ा ‘सब्रो-तक़सीम’ है। यह लगभग वही चीज़ है जिसको अंग्रेज़ी में process of elimination कहते हैं। यानी इन तमाम सम्भावित गुणों और स्थितियों की पहले निशानदेही की जाए जो इल्लत बन सकते हैं। फिर एक-एक करके उनकी अयोग्यता का फ़ैसला किया जाए। जो गुण अयोग्य होने से बच जाए वही इल्लत है।
दूसरा मशहूर तरीक़ा ‘मुनासबत’ है जिसके पाँच दर्जे हैं। इन पाँचों दर्जों का सम्बन्ध ‘मस्लहत’ (निहितार्थ) और ‘मुफ़सिदा’ (ख़राबी) से है। जिस सम्भावित गुण से कोई शरई मस्लहत जुड़ी हो या जिसके कारण कोई बड़ा बिगाड़ दूर होता हो उसको ‘इल्लत’ माना जाएगा।
इल्लत के निर्धारण के अन्य तरीक़ों में ‘दौरान’ का तरीक़ा भी शामिल है। लेकिन ये तरीक़े सर्वसम्मत नहीं हैं। इसलिए उनको मैं छोड़ देता हूँ। बहुत-से विद्वानों ने इल्लत के निर्धारण की प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया है। ये चरण या दर्जे जिनके लिए ‘मजारिल- इज्तिहाद फ़ी तईईनुल-इल्लः’ की शब्दावली भी प्रयुक्त की जाती है, आम तौर पर ‘सब्रो-तक़सीम’ वाली शैली में अधिक प्रभावी और लाभकारी साबित होते हैं।
- तहक़ीक़े-मनात : यह सबसे पहला चरण है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि यह इल्लत विभिन्न आदेशों में कहाँ-कहाँ पाई जाती है।
- तनक़ीहे-मनात : यह पता चलाने की कोशिश कि आदेश के विभिन्न गुणों और स्थितियों में से कौन-सा गुण इल्लत हो सकता है।
- तख़रीजे-मनात : अन्ततः इल्लत का पता चलाना।
‘इस्तेहसान’ क़ानून के स्रोत के तौर पर
‘क़ियास’ के बाद ‘इस्तेहसान’ है जो फ़िक़्ह के दूसरे स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ‘इस्तेहसान’ को सबसे पहले हनफ़ी फ़ुक़हा ने खोजा था। शुरू-शुरू में शेष फ़ुक़हा ने इस बारे में हनफ़ी फ़ुक़हा के साथ मतभेद किया और ‘इस्तेहसान’ को बतौर फ़िक़्ह के स्रोत के स्वीकार करने में संकोच किया। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने ख़ास तौर पर मतभेद किया और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के दृष्टिकोण के खंडन में किताब ‘इब्तालुल-इस्तिहसान’ के नाम से एक किताब लिखी। इमाम शाफ़िई (रह॰) के सामने ‘इस्तेहसान’ का जो विवरण किसी ने बयान किया वह हनफ़ी फ़ुक़हा की ‘इस्तेहसान’ की परिकल्पना से भिन्न था। उस विवरण के लिहाज़ से उसको ग़लत ही होना चाहिए। इमान शाफ़िई (रह॰) से किसी ने कहा कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) यह फ़रमाते हैं कि जहाँ क़ुरआन और सुन्नत में कोई आदेश न हो और ‘क़ियास’ के परिणामस्वरूप कोई मुश्किल मालूम हो तो अपनी पसंद के अनुसार फ़ैसला कर लो कि जो चीज़ अच्छी लगे उसको अपना लो। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने इसपर बहुत नापसंदीदगी का इज़हार किया और ज़ाहिर है हर मुसलमान ऐसा ही करेगा। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने फ़रमाया कि “जो ‘इस्तेहसान’ करता है वह स्वयं शरीअत का मालिक बनना चाहता है।” लेकिन इमाम शाफ़िई (रह॰) के बाद जब शेष शाफ़िई फ़ुक़हा को पता चला कि ‘इस्तेहसान’ वास्तव में किसको कहते हैं और इससे हनफ़ी फ़ुक़हा की मुराद क्या है तो फिर शाफ़िई फ़ुक़हा ने भी इससे सहमति जताई और बाद में तमाम फ़ुक़हा ने ‘इस्तेहसान’ को क़ानून के एक स्रोत के तौर पर व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
अगर आप अंग्रेज़ी क़ानून से परिचित हैं तो ‘इस्तेहसान’ लगभग वही चीज़ है जिसको Equity कहते हैं। एक्विटी और ‘इस्तेहसान’ लगभग एक ही चीज़ हैं। ये दोनों अगरचे मिलती-जुलती चीज़ें हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि ये दोनों सौ प्रतिशत एक नहीं हैं। कभी-कभी ‘क़ियास’ ऐसा होता है कि इसके जो परिणाम निकलते हैं तो वे शरीअत की नज़र में पसंदीदा नहीं होते। बज़ाहिर आपने अपनी समझ से जो ‘क़ियास’ किया वह आपको नियमों के अनुसार कलात्मक रूप से तो दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन जब उसको हालात पर चस्पाँ किया तो उससे ऐसे परिणाम निकले जो शरीअत से मेल नहीं खाते। अब ज़ाहिर बात है कि या तो आपका ‘क़ियास’ ग़लत है या वे परिणाम जो निकल रहे हैं वे दुरुस्त नहीं हैं। आपने ग़ौर किया तो ‘क़ियास’ की प्रक्रिया में कोई ग़लती मालूम नहीं होती। परिणाम देखते हैं तो शरीअत के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। आपने और अधिक ग़ौर किया तो महसूस हुआ कि एक अधिक सूक्ष्म और गुप्त subtle प्रकार का ‘क़ियास’ निकला जिसको अपनाने से वे समस्याएँ पैदा नहीं होती। इसलिए आपने ‘क़ियासे-जली’ यानी ज़ाहिरी ‘क़ियास’ को छोड़कर ख़ुफ़िया ‘बातिनी क़ियास’ को प्राथमिकता दी, इसलिए कि ‘क़ियासे-ज़ाहिरी’ से जो मुश्किल पैदा हुई है उसको दूर किया जाए, इस प्रक्रिया को ‘इस्तेहसान’ कहते हैं। यह बड़ा मुश्किल काम है। आसान काम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि ‘इस्तेहसान’ से काम लेनेवाला फ़क़ीह शरीअत से भी परिचित हो, अपने काम से भी परिचित हो और समस्याओं से भी परिचित हो। शरीअत की रूह से भी वाक़िफ़ हो।
कभी-कभी स्वयं शरीअत ने इस कार्य की गुंजाइश रखी है। और कुछ आदेशों में ‘इस्तेहसान’ से काम लिया है। उदाहरण के रूप में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद नहीं है उसको मत बचो।” अब यह एक मौलिक सिद्धान्त है। लेकिन अगर आप किसी सप्लायर को जाकर पैसे दे दें कि मुझे अपनी संस्था के लिए सौ कुर्सियाँ बनवानी हैं। तो वह आपसे पैसे ले-लेगा और कुर्सियाँ निर्धारित अवधि में सप्लाई कर देगा। लेकिन जब ज़रा ग़ौर करके देखें तो पता चलेगा कि आपने उससे यह मामला किया और रक़म अदा की तो उसके पास कुर्सियाँ मौजूद नहीं थीं। हदीस के ज़ाहिरी अर्थ के अनुसार तो यह अमल नाजाइज़ होना चाहिए था। इसलिए कि सप्लायर के पास वह चीज़ मौजूद नहीं जो वह बेच रहा है। यह इस हदीस के ज़ाहिरी अर्थ के अनुसार शरई आदेश का उल्लंघन है। लेकिन जब फ़ुक़हा ने इस मसले पर ग़ौर किया तो पता चला कि कारोबार और लेन-देन का यह तरीक़ा तो सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने से जारी था। सप्लायर उस ज़माने में भी हुआ करते थे। अगर इस हदीस का वही अर्थ होता तो बज़ाहिर समझ में आ रहा था तो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) उसका यही अर्थ क़रार देते और उनके ज़माने में यह काम बंद हो जाता। चुनाँचे इसपर फ़ुक़हा ने और भी ग़ौर किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि यह बैए-सुलिम का एक प्रकार है जो आम ‘क़ियास’ से तय नहीं होगा। इसको ‘क़ियासे-ख़फ़ी’ के आधार पर तय किया जाएगा। यह ‘इस्तेहसान’ का एक प्रकार है। इसको ‘इस्तेहसान-बिन-नस्स’ कहा जाता है कि ‘नस्स’ ने ‘इस्तेहसान’ से काम लिया और इस अमल की अनुमति दे दी, क्योंकि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में यह तरीक़ा प्रचलित था। वरना ज़ाहिरी तौर पर देखें तो यह अमल नाजाइज़ क़रार पाता है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी बड़ी मुश्किल की वजह से पवित्र क़ुरआन कोई आसानी पैदा कर देता है। इस आसानी को आप ‘क़ियास’ के अनुसार देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह आसानी किस आधार पर दी गई, न यह आसानी कलात्मक और ‘ज़ाहिरी-क़ियास’ के अनुसार प्रयुक्त की जा सकती है। अत: अगर ‘ज़ाहिरी क़ियास’ पर अमल करेंगे तो मुश्किल पैदा होगी। ‘क़ियास’ को छोड़ दें तो फिर क्या करें। ऐसे में ‘इस्तेहसान’ की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के रूप में एक तरफ़ हदीस में आता है कि हर उस जानवर का झूठा हराम है जो पंजेवाला हो और शिकार करके खाता हो इसलिए कि उसके मुँह में नापाक जानवर का ख़ून लगा होता है। दूसरी तरफ़ बिल्ली के झूठे को नापाक क़रार नहीं दिया गया। हालाँकि जब नापाक जानवर का ख़ून मुँह में लगने का अंदेशा हो तो क्या पता कि जब उसने बर्तन में मुँह डाला तो ख़ून लगा हुआ था या नहीं। उसका मुँह पाक था कि नापाक था। इसके विपरीत जो जानवर गोश्त नहीं खाते उनके मुँह में नापाक ख़ून लगे रहने की कोई सम्भावना नहीं। उनका झूठा नापाक नहीं। उदाहरणार्थ बकरी का मुँह तो पाक होता है क्योंकि वह घास खाती है और कोई नापाक चीज़ नहीं खाती। मुँह डाल लेगी तो पानी नापाक नहीं होगा। इसके विपरीत अगर कुत्ता या बिल्ली बर्तन में मुँह डाल ले तो इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वह कोई हराम जानवर खाकर आई हो और मुँह में ख़ून लगा रह गया हो। इसी तरह और कोई जानवर उदाहरणार्थ भेड़िया, शेर या इस तरह का कोई शिकारी जानवर अगर मुँह डाल दे तो उसका झूठा हराम होगा। लेकिन बिल्ली और दूसरे शिकारी और मांसाहारी जानवरों में अन्तर यह है कि बिल्ली हर घर में पाई जाती है। लोग उसको पालते भी हैं और अगर पाली न भी हो तो घरों में आसानी से घुस जाती है और पानी में या किसी और चीज़ के बर्तन में मुँह डाल देती है। तो अब अगर आदेश यह हो कि बिल्ली के मुँह डालने से चीज़ नाजायज़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, ख़ास तौर पर उन बस्तियों और आबादियों में जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ग़ौर किया तो पवित्र क़ुरआन की एक आयत उनके सामने आई जिसमें पर्दे का आदेश है कि अमुक से पर्दा करो, अमुक से पर्दा करो और अमुक-अमुक से न करो तो कोई हरज नहीं। सूरा-24 (नूर) में उल्लिखित है कि वे दिन-रात तुम्हारे पास आते-जाते रहते हैं, और हर वक़्त के आने-जानेवाले से बचना मुश्किल है इसलिए गुंजाइश है। तो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और फ़ुक़हा ने इस आयत की रौशनी में यह सोचा कि बिल्ली हर वक़्त घरों में आती-जाती है और उससे बचना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने यह क़ैद लगा दी कि अगर यह निश्चित हो जाए कि बिल्ली कोई ऐसा जानवर खाके आई है कि उसके मुँह में नापाक ख़ून लगा हुआ है और उसकी पुष्टि हो जाए कि उस समय ख़ून लगा हुआ था तो फिर पानी नापाक क़रार पाएगा वरना उस पानी को पाक समझा जाएगा, इसलिए कि बिल्ली “हर वक़्त आने-जानेवालों” में से है। यह भी ‘इस्तेहसान’ का एक उदाहरण है।
पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के इस तरह के उदाहरणों को सामने रखकर पहले हनफ़ी फ़ुक़हा ने और बाद में दूसरे फ़ुक़हा ने, ‘इस्तेहसान’ के विस्तृत नियम तैयार किए। उन्होंने ‘इस्तेहसान’ के बहुत-से प्रकार भी बयान किए। ‘इस्तेहसान’ के महत्वपूर्ण प्रकार ये हैं—
1. ‘इस्तेहसान बिन-नस्स’
जहाँ नस्से-शरई (क़ुरआन या हदीस के स्पष्ट आदेश) ने स्वयं ही किसी आम उसूल से किसी चीज़ को इसलिए अलग कर दिया हो कि इस चीज़ पर आम उसूल को चस्पाँ करने से कोई बुराई पैदा होने की सम्भावना हो, उदाहरणार्थ कोई असाधारण दिक़्क़त पैदा हो रही हो, या उसके परिणामस्वरूप लोगों के लिए कोई बड़ी परेशानी पैदा हो जाने का सख़्त ख़तरा लगा हुआ हो। इसका उदाहरण मैं दे चुका हूँ कि किस तरह शरीअत ने “जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद नहीं उसको मत बेचो” के नियम से ‘बैए-सुलिम’ को अलग किया है। ‘बैए-सुलिम’ यह है कि आप किसी सप्लायर को आज रक़म दे दें और वह बाद में किसी निर्धारित समय पर आपका दरकार माल, निर्धारित शर्तों पर उपलब्ध कर दे। सैद्धान्तिक रूप से यह चीज़ जायज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीअत ने बतौर ‘इस्तेहसान’ इस ख़ास कारोबार को जायज़ क़रार दिया और ‘बैए-सुलिम’ को इस आम उसूल से अलग कर दिया। यह ‘इस्तेहसान बिन-नस्स’ है।
2. ‘इस्तेहसान बिल-इजमा’
यह ‘इस्तेहसान’ का दूसरा प्रकार है, जहाँ इस्लाम के मुज्तहिदीन ने सर्वसहमति से किसी अधिक ज़ाहिर ‘क़ियास’ को नज़रअंदाज़ करके अधिक गुप्त ‘क़ियास’ को अपनाया हो। उदाहरणार्थ ‘बैए-सुलिम’ पर ‘क़ियास’ करके ‘अक़्दे-इस्तिसनाअ’ को जायज़ क़रार देना।
3. ‘इस्तेहसाने-क़ियासी’
यह ‘इस्तेहसान’ का तीसरा प्रकार है। इसमें ‘क़ियासे-ख़फ़ी’ को ‘क़ियासे-जली’ पर प्राथमिकता दी जाती है।
4. ‘इस्तेहसाने-ज़रूरत’
इसमें शरई आवश्यकता या मजबूरी की कैफ़ियत में किसी अधिक स्पष्ट उसूल के बजाय, मामले को तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट सिद्धान्त पर तय किया जाता है।
5. ‘इस्तेहसान’ उमूमे-बलवी के रूप में
यानी किसी ऐसी कमज़ोरी या ख़ामी को बर्दाश्त कर लेना जिसको ख़त्म करने की कोशिश से कोई बड़ी तकलीफ़ या ख़राबी जन्म लेती हो।
6. ‘इस्तेहसाने-उर्फ़ो-आदात’
आम रिवाज को देखते हुए किसी कलात्मक या टेक्निकल तक़ाज़े को नज़रअंदाज़ करना।
7. ‘इस्तेहसाने-हाजत’
लोगों की आम ज़रूरतों की रियाइत करते हुए किसी आदेश पर अमल करने में ज़्यादा सख़्ती से काम न लेना। ‘इस्तेहसान’ की बहसें अत्यंत नाज़ुक और मुश्किल हैं। ‘इस्तेहसान’ से काम लेना हर किसी ऐरे-ग़ैरे के बस की बात नहीं। इस काम के लिए फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह में असाधारण दक्षता, शरीअत के आदेशों और शरई क़ानूनों की तत्वदर्शिता में उच्च कोटि की अन्तर्दृष्टि और दीनी मामलों में आला दर्जे का एहसासे-ज़िम्मेदारी दरकार है। इन शर्तों के बिना ‘इस्तेहसान’ की संवेदनशील ज़िम्मेदारी उठाने का दुस्साहस करना दीन (इस्लाम) के साथ खिलवाड़ करने के समान है।
‘मस्लहत’ क़ानून के स्रोत के रुप में
फ़िक़्ही आदेशों का एक महत्वपूर्ण स्रोत ‘मसालेह-मुर्सला’ हैं। यानी उन निहितार्थों का ध्यान रखना जिनके बारे में शरीअत ने उम्मत को आज़ादी दी हो।
‘मस्लहत’ के आधार पर सबसे पहले मालिकी फ़ुक़हा ने फ़िक़ही आदेश संकलित करने और ‘मस्लहत’ को इज्तिहाद के आधार बनाने की शुरुआत की। बाद में दूसरे फ़िक़ही मसलकों ने भी ‘मस्लहत’ को बतौर इज्तिहाद के एक स्रोत या फ़िक़्ह के स्रोत के तौर पर स्वीकार कर लिया। इमाम ग़ज़ाली ने ‘अल-मुस्तसफ़ा’ में ‘मस्लहत’ की परिभाषा करते हुए कहा है कि हर वह चीज़ जो नीचे लिखे पाँच उद्देश्यों में किसी एक या सब की रक्षा और तरक़्क़ी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हो, वह ‘मस्लहत’ है।
- दीन की सुरक्षा
- जान की सुरक्षा
- नस्ल की सुरक्षा
- बुद्धि की सुरक्षा
- माल की सुरक्षा
और जिस चीज़ से ये उद्देश्य या उनमें से कोई एक प्रभावित या समाप्त होता हो वह बिगाड़ पैदा करनेवाला है। ऐसे हर बिगाड़ करनेवाले को रोकना और उसको ख़त्म करने की कोशिश करना भी ‘मस्लहत’ है।
मालिकी फ़ुक़हा प्रायः ‘मस्लहत’ के लिए ‘मस्लहते-मुर्सला’ या बहुवचन में ‘मसालेह-मुर्सला’ की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। उनके नज़दीक ‘मस्लहते-मुर्सला’ की परिभाषा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जटिल और सूक्ष्म है। वे कहते हैं कि ‘मस्लहते-मुर्सला’ से मुराद हर वह लाभ और लाभकारी चीज़ है जिसके बारे में शरीअत चुप हो, न शरीअत ने इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हो और न स्पष्ट रूप से उसको व्यर्थ और ग़लत क़रार देकर उसकी मनाही की हो। यह दो शर्तें इसलिए ज़रूरी हैं कि हर व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहे कि ‘मस्लहत’ के उसूलों से केवल उसी समय काम लिया जाएगा जहाँ फ़िक़्ह के सर्वप्रथम स्रोत क़ुरआन, सुन्नत, इजमा और इज्तिहाद ख़ामोश हों। इसके अलावा जिस चीज़ को शरीअत स्पष्ट रूप से ‘मस्लहत’ स्वीकार करती हो तो वह पहले ही शरई आदेश है और इसपर कार्यान्वयन सीधे पवित्र क़ुरआन या सुन्नते-रसूल के प्रमाण के आधार पर किया जाना ज़रूरी होगा। इस तरह जिस चीज़ को शरीअत ने ‘मस्लहत’ स्वीकार करने से पहले ही इनकार कर दिया हो उसको ‘मस्लहत’ समझने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अत: मुर्सला की शर्त अत्यन्त उचित है।
मालिकी फ़ुक़हा ने जायज़ ‘मस्लहत’ के निर्धारण के तीन पैमाने क़रार दिए हैं जिनको सामने रखकर ही किसी कार्य के ‘मस्लहत’ होने का फ़ैसला किया जा सकता है।
- वह कार्य कोई हक़ीक़ी और वास्तविक उपयोगिता या लाभ रखता हो। उसमें बयान की गई उपयोगिता मात्र काल्पनिक और अवास्तविक न हो।
- वह दरकार अवास्तविकता तमाम मुसलमानों के लिए हो, किसी ख़ास गिरोह या व्यक्ति के लिए न हो।
- वह कार्य क़ुरआन और सुन्नत की किसी ‘नस्स’ या इजमा से टकराता न हो।
उर्फ़ और रिवाज बतौर क़ानूनी स्रोत
फिर किसी समाज के उर्फ़ यानी रिवाज को भी शरीअत स्वीकार करती है। हर समाज में कुछ ख़ास तरीक़े होते हैं। शरीअत किसी सामाजिक रिवाज और तौर-तरीक़े को अकारण नहीं रोकती। किसी समाज में शलवार क़मीज़ पहनने का रिवाज है किसी समाज में जुब्बा और अबा पहनने का रिवाज है। किसी इलाक़े में चावल खाने का रिवाज है। किसी देश में गेहूँ पसंद किया जाता है। दुनिया में तरह-तरह के रिवाज, कारोबार के तरीक़े, लेन-देन के शिष्टाचार और मेल-जोल के तरीक़े होते हैं। बहुत-से फ़िक़ही आदेश ऐसे हैं जो इन तौर-तरीक़ों पर आधारित होते हैं। यह तौर-तरीक़े हर ज़माने के हिसाब से बदलते रहते हैं। चुनाँचे शरीअत के वे आदेश जिनका सम्बन्ध तौर-तरीक़ों से हो वे भी बदल जाएँगे। केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है कि जब नमाज़ पढ़ो तो पूरी ज़ीनत धारण करो। हर नमाज़ के समय पूरा लिबास पहनो। इस बारे में प्रतिष्ठित फ़ुक़हा ने सर्वसम्मत रूप से कहा है कि नमाज़ पढ़ते समय इंसान के लिए जहाँ तक सम्भव हो पूरा लिबास पहनना चाहिए। तहबंद बाँधकर भी और बनियान उतारकर भी नमाज़ पढ़ी जाएगी तो नमाज़ हो तो जाएगी, लेकिन ऐसा करना नमाज़ के अदब के ख़िलाफ़ है। नमाज़ का पूरा सम्मान और अदब यही है कि नमाज़ पढ़ते समय पूरा लिबास होना चाहिए।
अब पूरा लिबास क्या है। पश्चिमी जगत् में, यानी स्पेन, पुर्तगाल, उंदलुस, मराक़श (मोराको) आदि में, शुरू से यह रिवाज रहा है कि बुज़ुर्गों के सामने सिर ढाँपकर नहीं जाया जाता। यानी अपने बड़ों और सम्माननीय लोगों और बुज़ुर्गों के पास जाने का अदब यह था कि नंगे-सिर जाया जाए। आज भी पश्चिम में यही रिवाज है कि किसी बड़े और आदरणीय व्यक्ति के पास जाते हैं तो इज़्ज़त के लिए टोपी उतार देते हैं। या किसी को सलाम करना हो तो कहते हैं Hats off to you. पश्चिमी जगत् के इस रिवाज के आधार पर फ़ुक़हा ने लिखा है कि पश्चिम में यानी चीन, उंदलुस और पुर्तगाल वग़ैरा में नंगे सिर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। और पूरब में चूँकि रिवाज इसके विपरीत है। चूँकि यहाँ पुरुषों के लिए सिर ढकना अदब में शामिल समझा जाता है इसलिए यहाँ सिर ढाँपकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। यह अन्तर है जो उर्फ़, आदत या रिवाज के बदलने से पैदा होता है।
फ़ुक़हा ने लिखा है और शरीअत का उसूल है कि आपस की रज़ामंदी के बिना तिजारत दुरुस्त नहीं। क़ुरआन में आया है कि “यह और बात है कि तुम्हारी आपस की रज़ामन्दी से कोई सौदा हो।” (क़ुरआन, 4:29) फ़ुक़हा ने लिखा है कि तराज़ी (आपसी सहमति) की दलील यह है कि ‘ईजाब’ और ‘क़ुबूल’ हो। आपसे मैं कहूँ कि यह गिलास मुझे दस रुपये में बेच दें। आप कहें कि मैंने बेच दिया। यह तो ‘ईजाब’ और ‘क़ुबूल’ है और ‘तराज़ी’ की दलील है। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता। आदमी दुकान में जाकर दस रुपये रख देता है और चीज़ उठाकर ले आता है। अख़बारवाला बैठा होता है और आप पैसे रखकर अख़बार उठा लेते हैं। इसमें न ‘ईजाब’ है न ‘क़ुबूल’ है। यहाँ बज़ाहिर उसकी सम्भावना मौजूद है कि ‘तराज़ी’ न पाई जाए। इसकी सम्भावना मौजूद है कि उसने यह अख़बार नुमाइश के लिए रखा हो, बेचने के लिए न रखा हो। लेकिन चूँकि रिवाज है और सब इसको जायज़ समझते हैं और बेचनेवाला भी इससे सहमत है और ख़रीदार को भी पता है कि यह लेना और देना दोनों पक्षों की रज़ामंदी ही से हो रहा है इसलिए यहाँ विधिवत रूप से ‘ईजाब’ और ‘क़ुबूल’ का ज़बान से होना ज़रूरी नहीं। यह एक उर्फ़ है जिसके आधार पर समझा जाएगा कि ‘तराज़ी’ मौजूद है। इस तरह के आदेश हैं जो उर्फ़ और रिवाज के बदलने से बदल जाते हैं।
उर्फ़ का उसूल न केवल इस्लामी शरीअत ने, बल्कि दुनिया के अधिकतर क़ानूनों ने बतौर क़ानूनी स्रोत के स्वीकार किया है। उर्फ़ से मुराद वह रिवाज और कार्य-पद्धति है जो किसी क़ौम या इलाक़े में प्रचलित हो, लोग इससे अच्छी तरह परिचित हों और उस क़ौम या इलाक़े में उसको एक जायज़ और पसंदीदा रिवाज के तौर पर माना और बरता जाता हो। शरीअत में भी वे तमाम आदेश जो किसी क़ैद या शर्त के बिना दिए गए हों, जिनका न तो शरीअत में कोई विस्तृत निर्देश दिया गया हो और न अरबी भाषा में कोई एक निश्चित और अन्तिम रूप इसपर अमल दरआमद के लिए निर्धारित हो, उनका अर्थ उर्फ़ ही की रौशनी में निर्धारित किया जाएगा।
उर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल जिन फ़िक़ही अध्यायों में होता है वे ये हैं—
- क़सम और हलफ़ के मामलात। इन मामलात में क़सम खानेवाले के शब्दों और इबारतों का अर्थ उर्फ़ की रौशनी में तय किया जाएगा।
- तलाक़
- दआवा (दावे)
- बैअ (विक्रय)
उर्फ़ का अन्य विवरण और उप प्रकारों को मैं छोड़ देता हूँ। उर्फ़ के मूल आदेशों का सारांश ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ के आरम्भिक भाग में ‘क़वाइदे-फ़िक़हीया’ के स्न्दर्भ में आ गया है। और अधिक विस्तृत विवरण मुजल्ले की व्याख्याओं में देखा जा सकता है।
उर्फ़ के अलावा दो और महत्वपूर्ण मूल स्रोत ‘इस्तिसहाबुल-हाल’ और ‘शराए-साबिक़ा’ हैं। ‘इस्तिसहाब’ वास्तव में फ़िक़्ह के स्रोत से ज़्यादा अदालती कार्य-पद्धति के लिए एक उसूल या निर्देश है। इसका अर्थ यह है कि जो चीज़ पहले यानी बीते समय में साबित हो चुकी हो उसके बारे में माना जाएगा कि वह आज वर्तमान में भी शेष है जब तक कि किसी पक्की दलील से उसका मौजूद न होना और ख़त्म हो जाना साबित न हो जाए।
उसूले-ताबीरो-तशरीह (व्याख्या के सिद्धान्त)
उसूले-फ़िक़्ह का तीसरा बड़ा विषय दलालात यानी उसूले-ताबीरो-तशरीह (व्याख्या का सिद्धान्त) है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उसूले-फ़िक़्ह का वह मैदान जिसकी सबसे पहली ईजाद और आरम्भिक संकलन और विकास का सेहरा केवल उलमाए-उसूल के सिर है। ज्ञान का यह विभाग इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह की देन और प्रदान है। उलमाए-उसूल ने आज से एक हज़ार, बल्कि बारह सौ वर्ष पहले ही इस ज्ञान के इस विभाग को संकलित और व्याख्यायित कर दिया था। सच तो यह है कि उलमाए-उसूल से पहले किसी ने यह कला इतनी व्यापकता और मेहनत से संकलित ही नहीं की।
इस ज्ञान के आरम्भिक सिद्धान्त पहले-पहले क़ुरआन की टीका करने और क़ुरआन को समझने के उद्देश्य से संकलित किए गए। फिर क़ुरआन की टीका करने के लिए तैयार किए जानेवाले ये उसूल हदीस को समझने के लिए भी बरते जाने लगे। ज्यों-ज्यों ये नियम संकलित होकर और लिख-लिखकर सामने आते गए, इनसे काम लेने का दायरा भी फैलता रहा। पहले प्रतिष्ठित फ़ुक़हा की इबारतों, फिर आम क़ानूनी दस्तावेज़ों और आख़िर में हर क़ानून और क़ानूनी नियम की व्याख्या में इनसे काम लिया जाने लगा। यहाँ दलालात और उसूले-तफ़सीर की विस्तृत बहस तो सम्भव नहीं, इसलिए कि यह एक बहुत ही पेचीदा और गूढ़ विषय है। अलबत्ता संक्षिप्त रूप से बतौर परिचय, बल्कि बतौर आरम्भिक परिचय कुछ ज़रूरी बातें प्रस्तुत करता हूँ।
दलालात या नुसूस (स्पष्ट आदेशों) की व्याख्या के उसूलों में दो शैलियाँ जानी-मानी हैं—
- एक शैली ‘जमहूर’ कहलाती है।
- दूसरी शैली ‘अहनाफ़’ के नाम से जानी-जाती है।
‘जमहूर’ नामक शैली तुलनातमक रूप से ज़्यादा आसान और सबकी समझ में आनेवाली है, जबकि ‘अहनाफ़’ नामक शैली तुलनात्मक रूप से मुश्किल, लेकिन अधिक विस्तृत और गूढ़ है। ‘जमहूर’ नामक शैली के अनुसार किसी शरई, फ़िक़ही या क़ानूनी ‘नस्स’ में दो तरह के शब्द और इबारतें सम्भव हैं।
- मंतूक़ 2. मफ़हूम
‘मंतूक़’ वह है जिसको शरीअत बतानेवाले या फ़क़ीह ने प्रत्यक्ष रूप से अपने शब्दों में बयान किया हो। ‘मफ़हूम’ वह है जो सीधे शब्दों में तो बयान न हुआ हो, लेकिन शब्दों से उसका अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से निकलता हो। ‘मंतूक़’ की फिर दो क़िस्में हैं : ‘मंतूक़े-सरीह’ और ‘मंतूक़े-ग़ैर-सरीह’। इसी तरह ‘मफ़हूम’ की दो किस्में हैं ‘मफ़हूमे-मुवाफ़िक़’ और ‘मफ़हूमे-मुख़ालिफ़’। इन सबके बहुत-से उप प्रकार और अलग-अलग आदेश हैं।
‘अहनाफ़’ नामक शैली तुलनात्मक रूप से अधिक विस्तृत और अधिक पेचीदा और मुश्किल है। इसमें मौलिक चीज़ लफ़्ज़ियात और लफ़्ज़ियात के उप विभाजन हैं। यानी कोई शब्द किस अर्थ के लिए शब्दकोश में बनाया गया, इस दृष्टि से इसकी क़िस्में। किसी के अर्थ ज़ाहिर और छिपे हुए और अस्पष्ट हैं, इस दृष्टि से उसकी क़िस्में। किसी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हो रहा है, इस दृष्टि से उसकी क़िस्में। किसी शब्द के कौन-कौन-से अस्ली और उप-अर्थ निकलते हैं, इस दृष्टि से शब्द की क़िस्में। इन सबके अलग-अलग विस्तृत आदेश हैं। इन बहसों का सरसरी साराँश बयान करना भी एक लम्बा समय चाहता है। इसलिए इन बातों को परे करता हूँ।
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
Subscribe Our You Tube Channel
https://www.youtube.com/c/hindiislamtv
Recent posts
-
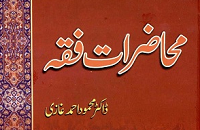
इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -
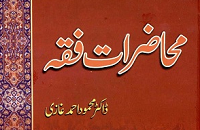
अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -
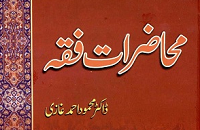
इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -
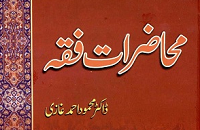
शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -
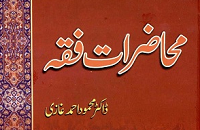
इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -
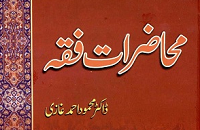
फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025

