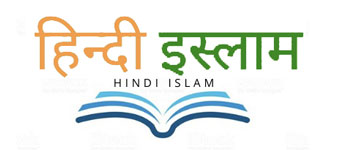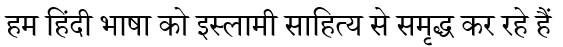इल्मे-फ़िक़्ह के विभिन्न विषय (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 4)
-
फ़िक़्ह
- at 25 February 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
फ़िक़ही उलूम से मुराद प्रायः फ़िक़्हे-इस्लामी और उसूले-फ़िक़्ह के वे अनगिनत उप-विभाग हैं जो पिछले चौदह सौ वर्षों के विकास और विस्तार के परिणामस्वरूप सामने आए हैं। जैसे-जैसे फ़िक़्हे-इस्लामी के मामलों और समस्याओं पर ग़ौर होता रहा, नई-नई तत्वदर्शिताएँ, नए-नए विभाग और नए-नए विषय सामने आते गए। अगर मानव-जीवन में विविधता है तो इंसान के वैचारिक और मानसिक प्रयासों में भी विविधता होगी। अगर मानव-जीवन में नई-नई समस्याएँ आए दिन सामने आ रही हैं तो फिर उनके नए-नए समाधान भी सामने आएँगे। इन समस्याओं पर ग़ौर करने के परिणामस्वरूप नित-नए जवाब भी सामने आएँगे। और जैसे-जैसे ये जवाबात संकलित होते जाएँगे तो उनसे नए-नए विभाग और ज्ञान की नई-नई शाखाएँ भी क़ायम होती जाएँगी। ऐसा हर ज्ञान और हर कला में होता है। विस्तार और विकास की यह प्रक्रिया हर मानवीय प्रयास और हर सांस्कृतिक प्रयास की विशेषता है। क़ुरआन की व्याख्या के ज्ञान के सन्दर्भ में ऐसा ही हुआ। हदीस और उलूमे-हदीस के मैदान में भी ऐसा ही हुआ। और मुसलमानों के हर मानसिक और वैचारिक प्रयास में ऐसा ही होता आया है।
चुनाँचे फ़िक़्हे-इस्लामी के नियम एवं सिद्धान्त तथा आदेशों पर जब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दौर में चिन्तन-मनन शुरू हुआ तो बहुत जल्द प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की फ़िक़ही अन्तर्दृष्टि ने फ़िक़्ह और शरीअत की तत्वदर्शिताओं और फ़तवों से ज्ञान-जगत् को माला-माल कर दिया। ताबिईन ने इस ज्ञान-संग्रह के संकलन का काम भी किया और इसे विस्तार भी दिया। ताबिईन का ज़माना समाप्त होने से पहले-पहले फ़िक़्हे-इस्लामी के अनेक विभाग अस्तित्व में आ गए। तबा-ताबिईन और उनके बाद आनेवाले इमामों और मुज्तहिदीन ने जैसे-जैसे फ़िक़ही मसाइल और आदेशों पर चिन्तन-मनन किया, उनका ध्यान नए-नए तथ्यों की ओर होता गया। इन नए-नए तथ्यों को नए आनेवालों ने संकलित किया। इस नए क्रम के परिणामस्वरूप बहुत-सी ऐसी शाखाएँ पैदा हो गईं जो क़ानून के विभिन्न मैदानों और पहलुओं की पहल करनेवाली बनीं। इन सब शाखाओं या उप-विभागों के संग्रह को फ़िक़्हे-इस्लामी कहा जाता है। आज जब फ़िक़्हे-इस्लामी की शब्दावली प्रयुक्त की जाती है तो इससे मुराद कोई एक ज्ञान या कोई एक कला नहीं होती, बल्कि इससे मुराद दर्जनों ज्ञान-विज्ञान और ज्ञान की दर्जनों शाखाओं का वह संग्रह होता है जिसपर फ़ुक़हा मुज्तहिदीन ने पूरे-पूरे पुस्तकालय तैयार करके रख दिए। यह केवल मुसलमानों में और फ़िक़्हे-इस्लामी के मामले में ही नहीं हुआ, बल्कि हर क़ौम और हर ज्ञान में ऐसा ही होता है। दुनिया की हर सभ्य क़ौम में ज्ञान के विस्तार और चिन्तन की गहराई के विभिन्न ढंगों और स्तर के उदाहरण बहुत अधिक पाए जाते हैं।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फ़िक़्ह से मुराद शरीअत के वे आदेश हैं जो इंसान के व्यावहारिक जीवन को संगठित और संकलित करते हों। वे आदेश जो शरीअत के विस्तृत तर्कों से उद्धृत हों। मानव-जीवन विभिन्न विभागों में विभाजित है। पवित्र क़ुरआन ने हर विभाग के बारे में मौलिक और सैद्धान्तिक निर्देश दिए हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनमें से हर विभाग में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का प्रशिक्षण किया। ऐसी छोटी-से-छोटी चीज़ें, जो आज हमें बज़ाहिर महत्वहीन और बहुत छोटी मालूम होती हैं, लेकिन जिनमें अल्लाह की तत्वदर्शिता ने यह उचित समझा कि इंसानों का मार्गदर्शन किया जाए, वहाँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इंसानों का मार्गदर्शन किया। केवल ज़ाहिरी चीज़ें देखनेवाले कुछ लोग शरीअत के आदेशों में कभी-कभी मामूली और छोटी-छोटी चीज़ों को देखकर यह आपत्ति कर दिया करते हैं कि एक आसमानी शरीअत में और फ़िक़्हे-इस्लामी के इतने सम्माननीय संग्रह में ये छोटी-छोटी और मामूली चीज़ें क्यों बयान की गई हैं? इस तरह की आपत्तियाँ करनेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि सर्वोच्च अल्लाह जो कायनात का रचयिता और इंसानों का शासक एवं मालिक है, वह इंसानों के साथ अत्यन्त स्नेही और दयालु भी है। वह अपनी रचना से अत्यन्त प्रेम करता है। अपनी रचना के साथ करुणामय भी है और दयावान भी है। इसलिए जहाँ-जहाँ उसके ज्ञान में यह बात थी कि यहाँ इंसानों की बुद्धि उनके मार्गदर्शन में ग़लती कर सकती है, वहाँ उसकी दयालुता से शरीअत ने एक मौलिक निर्देश दे दिया कि इंसान इस मामले में ग़लती न करने पाए।
यह आपत्ति कि शरीअत में छोटे-छोटे मामलों में मार्गदर्शन क्यों किया गया है, शरीअत की इसी तत्वदर्शिता को न समझने की वजह से है। यह आपत्ति आज से नहीं हो रही है, बल्कि स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुबारक ज़माने में भी लोगों ने यह आपत्ति करनी शुरू कर दी थी। सुनने-अबी-दाऊद की रिवायत है कि एक यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से व्यंग्य से कहा कि यह तुम्हारे नबी तुम्हें हगना, मूतना और इस्तिंजा करना भी सिखाते हैं? हज़रत सलमान फ़ारसी ने अत्यन्त गर्व से जवाब दिया कि जी हाँ, उन्होंने हमें इस्तिंजा के ये शिष्टाचार सिखाए हैं, तहारत (पाकी) के ये शिष्टाचार सिखाए हैं और अपने को पाक-साफ़ करने का यह और यह तरीक़ा बताया है। इससे अनुमान हो जाता है कि यह ग़लत-फ़हमी आज की नहीं है, बल्कि यह यहूदी ज़ेहन ने आज से चौदह सौ वर्ष पहले तराशी थी और हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसे सहाबी के सामने उसको पेश भी किया था।
मानव-जीवन बहुत बड़े-बड़े विभागों में विभाजित है। कुछ विभाग तो वे हैं जिनका सम्बन्ध अक़ीदों (धारणाओं) और इंसान की विचारधारा और उसकी वैचारिक समस्याओं से है। इन समस्याओं के बारे में निस्सन्देह शरीअत ने इंसानों का पूरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन जब फ़िक़्ह के आदेश एवं समस्याएँ ज़्यादा व्यापकता के साथ विकसित हुईं तो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इन मामलों को फ़िक़्ह के विशेष कार्य-क्षेत्र से बाहर क़रार दिया। यही हाल शरीअत के एक और महत्वपूर्ण मौलिक विभाग ‘तज़किया’ (व्यक्तित्व के निखार) और ‘एहसान’ (कार्य को फ़र्ज़ से बढ़कर उत्तम ढंग से करना) का है जो इंसानों की आन्तरिक अनुभूतियों और भावनाओं के सुधार के बारे में मार्गदर्शन उपलब्ध करता है।
फ़िक़्ह के महत्वपूर्ण और मौलिक अध्याय
आज फ़िक़्ह जिस अंदाज़ में हमारे सामने संकलित रुप में मौजूद है इसके कार्य-क्षेत्र में अक़ीदे और अनुभूतियाँ नहीं आतीं। भावनाएँ एवं अनुभूतियाँ और धारणाएँ एवं विचार की बहसें फ़िक़्ह के दायरे से बाहर हैं। एक ज़माने में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इन समस्याओं को भी फ़िक़्ह में शामिल समझा। चुनाँचे इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) से फ़िक़्ह की जो परिभाषा सम्बद्ध है और जो मैंने सम्भवत: पहले ही दिन की चर्चा में आपको सुनाई थी, वह यह है “इंसान को इस बात का ज्ञान कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और उसपर क्या-क्या चीज़ें अनिवार्य हैं? इस समझ का नाम फ़िक़्ह है।” इसमें इंसान और उसके जीवन से सम्बन्धित सब चीज़ें शामिल हैं। अक़ीदे (धारणाएँ) भी शामिल हैं। भावनाएँ एवं अनुभूतियाँ और नैतिक मूल्य एवं नैतिक आचरण भी शामिल हैं। चुनाँचे इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने सबसे पहले जो किताब ‘अल-फ़िक़्हुल-अकबर’ के नाम से लिखी इस में फ़िक़्ह का यही आम अर्थ सामने रखा गया। इस किताब में अक़ीदों और रवैये के बारे में बहुत-सी सैद्धान्तिक बातें कही गई हैं। बाद में जब विशिष्टता प्राप्त करने यानी specialization का दौर आया, और फ़िक़्ह का कार्य-क्षेत्र काफ़ी सीमित और अधिक स्पष्ट हो गया तो फिर फ़िक़्ह की शब्दावली केवल ज़ाहिरी कामों पर आधारित आदेशों के लिए प्रयुक्त होने लगी। ज़ाहिरी काम भी अनगिनत हैं। मानव-जीवन के हर क्षेत्र में ज़ाहिरी कर्म हैं, बल्कि ज़ाहिरी कर्मों ही से इंसान का जीवन भरा हुआ है।
मैंने बताया था कि अगर आप मानव-जीवन में पेश आनेवाली समस्याओं का क्रमानुगत जायज़ा लें तो क्रम में सबसे पहले तहारत (पाकी) की समस्याएँ आएँगी। इसके बाद ज़कात का मसला आएगा, उसके बाद रोज़े और उसके बाद हज का मसला आएगा। यह शरीअत की वे मौलिक समस्याएँ और आदेश हैं जिनसे हर मुसलमान को वास्ता पड़ता है। शेष मामलों से किसी मुसलमान को वास्ता शायद न पड़े। पंद्रह-सोला वर्ष की उम्र में एक बच्चा वयस्क हुआ। मान लीजिए कि शादी करने का मौक़ा ही नहीं मिला तो दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित आदेशों पर अमल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। या कोई व्यक्ति बुढ़ापे में मुसलमान हुआ। घरवालों को छोड़कर इस्लाम के वतन में आकर बस गया और दोबारा दाम्पत्य जीवन गुज़रने का मौक़ा नहीं मिला, या इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसे व्यक्ति के लिए दाम्पत्य जीवन के बहुत-से मामले व्यावहारिक आवश्यकता की समस्याएँ नहीं हैं। एक व्यक्ति ने ज़िंदगी-भर अपने बाप-दादा की विरासत और बचा हुआ पैसा खाया और उसको किसी व्यापार आदि की आवश्यकता नहीं पड़ी तो उसके लिए व्यापार के आदेश महत्वहीन होंगे और शायद जीवन के बहुत-से हिस्से में उसको व्यापार के आदेशों की व्यावहारिक रूप से आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन इबादतों के आदेश हर मुसलमान के लिए हर समय और हर हाल में ज़रूरी हैं। वे उसे अवश्य करने हैं। नमाज़ भी पढ़नी है, ज़कात भी देनी है, रोज़ा भी रखना है, और अगर संसाधन हैं तो हज भी करना है। इसलिए फ़िक़्ह का सबसे पहला मैदान इबादतें हैं।
इबादतों से मुराद वे सभी धार्मिक कृत्य एवं आदेश हैं जिनका सीधा उद्देश्य, ‘सीधा’ के शब्द पर ग़ौर कीजिएगा, जिनका सीधा उद्देश्य अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध को मज़बूत करना है। यों तो शरीअत के तमाम आदेशों का उद्देश्य अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध को मज़बूत करना है। आप बाज़ार में सौदा ख़रीदने जाएँ और यह ख़याल रखें कि शरीअत में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है तो इससे भी सम्बन्ध मज़बूत होता है। आप बच्चों का प्रशिक्षण इस ख़याल से करें कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बच्चों के अच्छे प्रशिक्षण का आदेश दिया है, तो यह विशुद्ध सांसारिक गतिविधि है, लेकिन इससे भी अल्लाह के साथ सम्बन्ध मज़बूत होता है।
लेकिन इन चीज़ों का सीधा, अस्ल और वास्तविक अभीष्ट अक्सर एवं अधिकतर सर्वोच्च अल्लाह से सम्बन्ध मज़बूत करना नहीं होता। किसी का यह इरादा और प्रेरणास्रोत होता है किसी का नहीं होता। लेकिन नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और शेष इबादतों का उद्देश्य केवल और केवल अल्लाह से सम्बन्ध मज़बूत करना ही होता है और कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए उनको ख़ालिस इबादतें कहा जाता है और यह फ़िक़्हे-इस्लामी का सबसे पहला अध्याय है। फ़िक़्हे-इस्लामी में इबादतों के अध्याय इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इतने विस्तार और मेहनत से लिखे हैं कि आज किसी इंसान को दुनिया के किसी कोने में नमाज़, रोज़ा और ज़कात के आदेश मालूम करने में कोई दिक़्क़त पेश नहीं आती। और आए दिन जैसे-जैसे समस्याएँ पैदा होती जा रही हैं, उनका जवाब अव्वल तो अइम्मा मुज्तहिदीन ही के यहाँ से मिल जाता है, वरना हर दौर के विद्वानों ने यह ज़िम्मेदारी अंजाम दी है। मानव-जीवन में प्रतिदिन समस्याएँ पैदा होती हैं, प्रतिदिन सवाल पैदा होते हैं, आज के विद्वान उनका जवाब इसी तरह देते हैं और आगे भी देंगे जिस तरह अतीत के विद्वान अतीत में देते चले आए हैं। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का सबसे पहला विभाग है। फ़िक़्ह की अक्सर किताबों में सबसे पहले इबादतों ही की बहस मिलती है।
इस्लाम का पारिवारिक क़ानून
इबादतों के बाद दूसरा बड़ा विभाग व्यक्तिगत और पारिवारिक क़ानूनों का विभाग है। जिसके लिए कुछ फ़ुक़हा ने ‘मनाकिहात’ की शब्दावली प्रयुक्त की है। यानी निकाह और उससे सम्बन्धित शिष्टाचार और आदेश। परिवार की संस्था अस्तित्व में कैसे आए और जब यह संस्था अस्तित्व में आ जाए तो उसके नियम और आदेश क्या होंगे? परिवार के व्यक्तियों के आपस के सम्बन्ध और मामलों का स्वरूप क्या होगा? ये वे चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत मामलों या ‘मनाकिहात’ में चर्चा में आती हैं।
अगर आप शूरू से आख़िर तक पवित्र क़ुरआन का एक-एक पेज देखकर जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि पवित्र क़ुरआन के आदोशों से सम्बन्धित आयतों में सबसे ज़्यादा ज़ोर इन्हीं दो विभागों पर दिया गया है। यानी इबादात और ‘मनाकिहात’ पर। लगभग डेढ़ सौ आयतें हैं जो इबादतों के बारे में हैं और क़रीब-क़रीब उतनी ही संख्या में आयतें व्यक्तिगत क़ानूनों के बारे में हैं। यानी निकाह, इससे सम्बन्धित, नफ़क़ा (गुज़ारे का ख़र्च), हज़ानत (गोद लेना), वलायत (वारिस बनना), तलाक़, विरासत और वसीयत वग़ैरा के बारे में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये दो विभाग वे हैं जो मानव-जीवन के व्यक्तिगत और सामूहिक पहलुओं को इस तरह संगठित और संकलित करने में मौलिक भूमिका निभाते हैं जिस तरह इस्लाम चाहता है। इसलिए पवित्र क़ुरआन में सबसे ज़्यादा ज़ोर इन्हीं दो विभागों पर दिया गया है। शेष विभाग भी व्यावहारिक जीवन ही से सम्बन्धित हैं और अपनी-अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन ये दो विभाग वे हैं जिनमें सबसे पहला विभाग इंसान यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की आध्यात्मिक पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दूसरा विभाग सामूहिकता की पहली ईंट को सही निर्देशों पर स्थापित करता है यानी परिवार।
पवित्र क़ुरआन से पता चलता है कि परिवार की संस्था इस्लाम में अत्यन्त मौलिक महत्व रखती है, अगर परिवार की संस्था मज़बूत है, इसका आधार गहरा है, इसका आधार शरीअत के आदेशों पर है, परिवार के व्यक्तियों के दरमियान सम्बन्ध के प्रकार और आधार नैतिक और आध्यात्मिक हैं, हया (शर्म) और इस्लाम के दूसरे नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है, तो ऐसे परिवारों से जो समाज अस्तित्व में आएगा वह एक इस्लामी समाज होगा जो पवित्र क़ुरआन का पहला उद्देश्य है। यहाँ यह बात याद रखिए कि पवित्र क़ुरआन का सबसे पहला सामूहिक लक्ष्य एक आदर्श इस्लामी समाज की स्थापना है। आदर्श इस्लामी समाज यानी मुस्लिम समाज का गठन ही पैग़म्बरों (अलैहिस्सलाम) का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने आज से पाँच हज़ार वर्ष पहले दुआ की थी कि “ऐ अल्लाह मेरी सन्तान में एक नबी पैदा कर और मेरी सन्तान से एक मुस्लिम समाज पैदा कर।” यह दुआ जो हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ने मिलकर उस समय माँगी थी जब वह बैतुल्लाह (काबा) की बुनियादें उठार रहे थे। यह बात बड़ा महत्व रखती है कि इस दुआ में किसी राज्य या साम्राज्य की स्थापना की दुआ नहीं माँगी गई थी, बल्कि मुस्लिम समाज के गठन की दुआ की गई थी। दोनों पैग़म्बरों ने दुआ माँगी थी, तो जिस उम्मत (समुदाय) की दुआ पाँच हज़ार वर्ष पहले की गई हो, जिस उम्मत की तैयारी के लिए यह सारी लम्बी अवधि गुज़री हो, जिसकी शरीअत और जिसकी जीवन व्यवस्था के लिए तैयारी करने में साढ़े तीन हज़ार वर्ष गुज़रे हों, वही उम्मत इस्लाम का सबसे पहला उद्देश्य है। इसी उम्मत की स्थापना शरीअत का मौलिक लक्ष्य है। इस उम्मत की रक्षा के लिए बहुत-से मौलिक आदेश दिए गए। पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में जितने सामूहिक आदेश दिए गए हैं वे इस उम्मत के रक्षा के लिए दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस उम्मत के लिए अपनी रातें दुआओं और अल्लाह से विनतियाँ करने में गुज़ारीं। उनके दिनों की मशक़्क़त और क़ुर्बानियाँ, उनकी रातों का दुआएँ माँगना, सब इसी उम्मत को अस्तित्व में लाने, इसका निर्माण करने और इसकी रक्षा को निश्चित बनाने के लिए था। इस उम्मत की ख़ातिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुत-सी क़ुर्बानियाँ दीं।
आपको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हर बक़र-ईद के मौक़े पर दो दुंबों की क़ुर्बानी करते थे। एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। हज्जतुल-विदा के मौक़े पर उन्होंने अपने मुबारक हाथ से त्रेसठ (63) ऊँट ज़बह किए। ये सब उम्मत की तरफ़ से थे। मैं कभी-कभी सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब कैफ़ियत पैदा होती है। ख़याल आता है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दुंबे की जो क़ुर्बानी की थी वह मेरी तरफ़ से भी थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मेरी तरफ़ से दुंबे को ज़बह किया था। इस क़ुर्बानी का एक अरबवाँ या दस खरबवाँ हिस्सा मुझे भी मिलेगा।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक-बार कहा कि “सर्वोच्च अल्लाह ने हर पैग़ंबर को यह अधिकार दिया कि कोई एक ऐसी दुआ करो जो तुरन्त स्वीकार कर ली जाए।” सर्वोच्च अल्लाह की रीति है कि वह दुआ स्वीकार करने में एक विशेष नियम की पाबन्दी करता है। इस नियम को छोड़ते हुए कम-से-कम एक मौक़ा हर पैग़ंबर को दिया गया कि आप उस समय जो कहेंगे वह तुरन्त कर दिया जाएगा। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा कि “क्या हर पैग़ंबर ने इस मौक़े से फ़ायदा उठाया?” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि “हाँ हर पैग़ंबर ने इससे फ़ायदा उठाया।” सहाबा ने पूछा कि आपने इस मौक़े पर क्या दुआ की और दुआ में सर्वोच्च अल्लाह से क्या माँगा? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि “मैंने इस मौक़े को आख़िरत के लिए उठा रखा है। मैं आख़िरत के मौक़े पर अपनी उम्मत के लिए दुआ करूँगा। सर्वोच्च अल्लाह ने इस एक दुआ की तुरन्त स्वीकृति का वादा किया है। तो जब एक दुआ की तुरन्त स्वीकृति का वादा किया है तो मैं क़ियामत के दिन पूरी उम्मत के लिए दुआ करूँगा।”
इस उम्मत की रक्षा के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक उन व्यक्तियों का प्रशिक्षण और गठन, जिनसे यह उम्मत अस्तित्व में आएगी। और उस ईंट की बनावट और उस ईंट का गठन जो उम्मत की सामूहिकता के निर्माण में पहले क़दम की हैसियत रखती है यानी परिवार। इसलिए पवित्र क़ुरआन में जितने भी व्यावहारिक आदेश हैं, उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग डेढ़ सौ आयतें व्यक्ति के बारे में हैं। इसलिए कि इबादतें व्यक्ति अंजाम देता है। हज मैं अपने लिए करूँगा आप अपने लिए करेंगे। नमाज़ मैं अपने लिए पढ़ता हूँ आप अपने लिए पढ़ते हैं। रोज़ा मैं अपने लिए रखूँगा आप अपने लिए रखेंगे।
व्यक्ति के बाद परिवार की संस्था है जिसकी रक्षा के लिए शरीअत ने इतने विस्तृत आदेश दिए हैं कि पवित्र क़ुरआन की डेढ़ सौ के क़रीब आयतें केवल व्यक्तिगत स्थिति और पारिवारिक व्यवस्था के बारे में हैं। यहाँ तक कि पवित्र क़ुरआन में आया है कि सर्वोच्च अल्लाह ने एक बार इंसानों की आज़माइश के लिए कि वे किस हद तक तौहीद (एकेश्वरवाद) और इस्लाम के अक़ीदे पर दृढ़ हैं, दो फ़रिश्तों को जादूगरों के भेस में भेजा। फ़रिश्तों ने लोगों से कहा कि हम जादू सिखाते हैं। देखना यह था कि कितने लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं और कितने बचते हैं। पैग़म्बरों के प्रशिक्षण और शिक्षा का कितना प्रभाव शेष है और कितनी जल्दी ये एक ऐसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार होते हैं जिसको पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) ने मना किया था। वह जादू जो आज़माइश के लिए उतारा गया था वह कोई ऐसा मंत्र था जिससे पति और पत्नी के बीच जुदाई पैदा होती थी; यह वह चीज़ है जिसको पवित्र क़ुरआन ने कुफ़्र बताया है। यह ग़लत हरकत जो लोगों ने सीखी, यह इस्लाम विरोधी जादूगरी यह थी कि पति और पत्नी के बीच मतभेद पैदा हो जाए। यानी यह इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पवित्र क़ुरआन ने इस चीज़ को रिकार्ड किया है कि पढ़नेवाले यह अनुमान रखें कि परिवार के दरमियान सम्बन्ध और स्थायित्व की क्या हैसियत है।
व्यक्तिगत स्थितियों या व्यक्तिगत क़ानूनों में मौलिक रूप से चार चीज़ें चर्चा में आती हैं। सबसे पहले यह बहस की जाती है कि परिवार की संस्था कैसे अस्तित्व में आए। परिवार की संस्था एक मीसाक़ (अनुबन्ध) के द्वारा अस्तित्व में आएगी। पवित्र क़ुरआन में अनुबन्ध के लिए अक़्द, अह्द और मीसाक़ की शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं। ‘अक़्द’ एक आम नागरिक या दीवानी अनुबन्ध यानी civil contract को कहते हैं। ‘अह्द’ इससे ज़रा बड़ा शब्द है जिसमें एक सिविल कंट्रैक्ट के साथ-साथ एक गहरा वादा या निजी commitment भी मौजूद हो, लेकिन ‘मीसाक़’ का शब्द बहुत गहरे और पक्के वादे के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तक कि अल्लाह और बन्दे के दरमियान जो वादा है उसके लिए मीसाक़ की शब्दावली प्रयुक्त हुई है। जहाँ ‘रोज़े-अलस्त’ (देखें, क़ुरआन, 7:172) के अह्दो-पैमान का ज़िक्र है, इसके लिए कुछ स्पष्ट आदेशों में मीसाक़ की शब्दावली प्रयुक्त हुई है। इसी तरह सर्वोच्च अल्लाह ने बनी-इसराईल से मीसाक़ यानी गहरा वादा लिया कि वे क्या रवैया और क्या कार्य-नीति अपनाएँगे। वह शब्दावली जो अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध के लिए प्रयुक्त हुई है, वही शब्दावली पति और पत्नी के दरमियान सम्बन्ध के लिए भी प्रयुक्त हुई है। पवित्र क़ुरआन ने मात्र मीसाक़ का शब्द प्रयुक्त करने पर बस नहीं किया, बल्कि मीसाक़ के साथ ‘ग़लीज़’ का शब्द भी प्रयुक्त किया है। ‘ग़लीज़’ के अरबी भाषा में वह अर्थ नहीं जो उर्दू में प्रचलित हो गए हैं। अरबी भाषा में ग़लीज़ का अर्थ है अत्यन्त मज़बूत, टिकाऊ, अत्यन्त सख़्त और अत्यन्त मोटी चीज़ जो तोड़ी न जा सके और जो नज़रों से ओझल न हो सके, जिसको नज़रअंदाज न किया जा सके, जिसे हराया न जा सके यानी तुम्हारे और तुम्हारी पत्नियों के दरमियान एक अटूट मीसाक़ मौजूद है। सर्वोच्च अल्लाह यह मीसाक़ क़ायम करना चाहता था। इसलिए परिवार की संस्था पर बड़ा ज़ोर दिया गया कि यह अस्तित्व में कैसे आएगी। और अस्तित्व में आने के बाद उसके परिणामस्वरूप जो अधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ पैदा होंगी वे क्या होंगी। अधिकार एवं दायित्वों पर कार्यान्वयन का तरीक़ा क्या होगा। इस बात को कैसे निश्चित बनाया जाएगा कि
परिजनों के अधिकार एवं कर्तव्य सुरक्षित हैं और उनका पालन किया जा रहा है।
फिर अगर किसी वजह से परिवार की संस्था सफल न हो सके और अन्ततः दोनों पक्ष यह महसूस करें कि वे अल्लाह की सीमाओं और उसकी शरीअत के अनुसार इस ‘अह्द’ की पाबन्दी नहीं कर सके जो उन्होंने किया था तो इसको समाप्त कैसे किया जाए। समाप्त करना भी शिष्टाचार और नैतिक आचरण के दायरे में रहते हुए अल्लाह के क़ानून के अनुसार होना चाहिए। पवित्र क़ुरआन में है कि अगर साथ रहना है तो अच्छे तरीक़े से साथ रहो, अलग होना है तो फिर अच्छे तरीक़े से और एक सभ्य ढंग से अलग हो जाओ। एक भले, उचित और शिष्ट तथा सदाचारी इंसान की तरह अलग हो जाओ। लड़-झगड़कर अलग मत हो। अपने गंदे कपड़े सड़क पर मत धोओ। अपने आपस के मतभेदों को ग़ैरों के सामने बयान न करो। मतभेद होते हुए, ख़ामोशी, सम्मान और इज़्ज़त एवं आबरू के साथ अलग हो जाओ। जब अलग हो जाओ तो फिर नैतिक आचरण और शरीअत के आदेशों की पैरवी करो। दोनों एक-दूसरे के मामले में लागू होनेवाली ज़िम्मेदारियों को उठाओ।
तीसरी चीज़ यह है कि परिवार की संस्था के परिणामस्वरूप सम्पत्ति पैदा होगी। इसमें से कोई सम्पत्ति साझी भी होगी। आज अगर साझी नहीं तो सम्भव है कि कल साझी हो जाए। उसके लिए इस्लामी शरीअत ने विरासत के आदेश दिए हैं। विरासत के आदेशों का मौलिक सिद्धान्त यह है और यह सिद्धान्त शरीअत के आदेशों का एक मौलिक सिद्धान्त भी है कि जिस चीज़ का फ़ायदा आप उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी या आप ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी व्यक्ति की कमज़ोरी या नादारी या बीमारी या बुढ़ापे में उसकी समस्याओं और मामलों के ज़िम्मेदार हैं और शरीअत यह ज़िम्मेदारी आपपर डालती है तो अगर उस व्यक्ति की कोई विरासत हो और वह कुछ छोड़कर चला जाए तो उसमें आपका भी हिस्सा है। यह नहीं हो सकता कि जब वह मुश्किल में हो तो सारी ज़िम्मेदारी आप पर हो और अगर उसके पास कोई सम्पत्ति या माल एवं दौलत हो तो उसमें आपको कोई हिस्सा न मिले। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। ‘अल-ख़िराज बिज़-ज़मान’ ये हदीस के शब्द हैं। फ़ायदे और तावान दोनों साथ-साथ चलते हैं। फ़ायदा और ज़िम्मेदारी साथ-साथ चलती हैं। जहाँ ज़िम्मेदारी होगी वहाँ फ़ायदा भी होगा और जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ ज़िम्मेदारी भी होगी। शरीअत की मूल आत्मा और न्याय एवं इंसाफ़ के अनुसार यह नहीं हो सकता कि एक चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तो आप आगे-आगे रहें और इससे ख़ूब लाभान्वित होते रहें, मगर जब ख़र्च करने और उसकी ज़िम्मेदारी निभाने का मौक़ा आए तो आप पीछे नज़र आएँ। या जब ख़र्च और ज़िम्मेदारी का मौक़ा आए तो आपको आगे कर दिया जाए और जब फ़ायदे का मौक़ा आए तो आपको पीछे कर दिया जाए। यह शरीअत के स्वभाव और न्याय एवं इंसाफ़ की कल्पना के विरुद्ध है।
पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है कि “और इसी तरह उसके वारिस पर भी ज़िम्मेदारी है, जैसी कि उसपर है,” (क़ुरआन, 2:233) यह वाक्य जिस सन्दर्भ में आया है वहाँ नफ़क़ा (गुज़ारा भत्ता) की ज़िम्मेदारियाँ बयान हो रही हैं कि अमुक की ज़िम्मेदारी यह है और अमुक की ज़िम्मेदारी यह है। बाप के ज़िम्मे है कि बच्चों का नफ़क़ा (ख़र्च) दे। पति के ज़िम्मे है कि वह पत्नी का ख़र्च बर्दाश्त करे। बाप के ज़िम्मे है कि उसके बच्चे जब तक अपने पाँव पर खड़े न हों उनका ख़र्च बर्दाश्त करे। अगर यह ज़िम्मेदारी बाप की है और बच्चे कुछ छोड़कर मरें और बाप ज़िन्दा है तो बच्चों के तरके में से बाप को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर बाप बूढ़ा है और बच्चे जवान हैं तो बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि बाप के ख़र्चे बर्दाश्त करें। और अगर बूढ़ा बाप कुछ छोड़कर मरा है तो उसमें से बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए। यानी फ़ायदा और ज़िम्मेदारी एक साथ चलती हैं और उनको एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए शरीअत ने कुछ मौलिक सिद्धान्त दिए हैं जिनकी रौशनी में विरासत के आदेश दिए गए हैं।
विरासत के सन्दर्भ में दुनिया की हर क़ानूनी व्यवस्था ने नाइंसाफ़ियाँ की हैं। दुनिया के हर धर्म, हर संस्कृति और हर सभ्यता ने विरासत के मामले में ठोकरें खाई हैं। हमारी बहुत-सी बहनें पश्चिम से आनेवाली हर चीज़ को आसमान से उतरी वह्य (ईश-प्रकाशना) के बराबर समझती हैं। पता नहीं उनमें से कितनों को पता है कि पश्चिम में आज भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको रिवायती अंग्रेज़ी क़ानून के अनुसार विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। एक वर्ग ऐसा है जिसमें क़ानून के अनुसार विरासत में से महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलता। विरासत के मालिक के करोड़ों के तरके (छोड़े हुए धन-सम्पत्ति) में से एक पैसा भी नहीं मिलता। हमारे देश में बहुत-सी महिलाओं को यह तो ख़ूब याद रहता है कि पवित्र क़ुरआन ने महिलाओं का हिस्सा कुछ जगह आधा रखा है। इसपर वह आए दिन आपत्ति भी करती रहती हैं, सीधे-सीधे पवित्र क़ुरआन पर आपत्ति करने की तो उनमें बहुत-सी महिलाओं को अभी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन मौलवियों को बुरा-भला कहती रहती हैं और इज्तिहाद के नाम पर विरासत के आदेशों में संशोधन की माँग करती रहती हैं। लेकिन ये महिलाएँ पश्चिम पर आपत्ति नहीं करतीं कि वहाँ औरत को विरासत से सिरे से ही वंचित क्यों कर दिया गया है। वहाँ Primogeniture का सिद्धान्त कार्यरत है। प्राइमोजेनिचर का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा बेटा वारिस होगा। इससे आगे बात ख़त्म। सबसे बड़े बेटे के अलावा हर व्यक्ति वंचित है। तमाम विरासत सबसे बड़े बेटे को मिलेगी। यह उसूल पहले पूरे इंग्लैंड और पूरे यूरोप में सौ प्रतिशत जारी था। अब पिछले पचास-साठ वर्षों से इसका दायरा ज़रा सीमित हो गया है, लेकिन अब भी वहाँ के लार्ड्ज़ और landed aristocracy से जुड़ जितने बड़े-बड़े लोग हैं वे इसी क़ानून का पालन करते हैं। भारत में भी अंग्रेज़ों के ज़माने में यह क़ानून मौजूद था। इसपर किसी ने कभी आपत्ति नहीं की, कभी किसी को यह बुरा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसा होता है। इसके विपरीत इस्लाम की हर चीज़ सोचे-समझे बिना ही आपत्तिजनक मालूम होती है।
सारांश यह कि शरीअत में विरासत के आदेशों के अनुसार जिन-जिनके हिस्से पवित्र क़ुरआन ने नियुक्त किए हैं उनको मिलेंगे। पवित्र क़ुरआन में हिस्से नियुक्त करने में मौलिक सिद्धान्त यह सामने रखा गया है कि किसकी ज़िम्मेदारी क्या है। जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और जिसकी ज़िम्मेदारी कम है उसे कम हिस्सा मिलेगा। कुछ जगहों पर पुरुष और औरत दोनों के लिए बराबर हिस्से नियुक्त है। दोनों को छटा हिस्सा मिलेगा यानी माँ को भी छटा हिस्सा मिलेगा और बाप को भी छटा हिस्सा मिलेगा। एक और स्थिति में बहन-भाइयों का हिस्सा बराबर है। दोनों को तरके (छोड़ी गई सम्पत्ति) का छटा-छटा हिस्सा मिलेगा। कुछ जगह औरतों को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और पुरुषों को कम हिस्सा मिलेगा। कुछ जगह पुरुषों को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और औरतों को कम हिस्सा मिलेगा। आप क़ुरआन की सूरा-4 निसा की वे आयतें तो कम-से-कम एक बार किसी अच्छी व्याख्या के साथ पढ़ लें, जिनमें विरासत के आदेश बयान हुए हैं, तो आदेशों की विभिन्न शक्लें मालूम हो जाएँगी और यह आपत्ति कि औरतों का हिस्सा हमेशा आधा और अकारण ही आधा होता है, इसकी कमज़ोरी स्पष्ट हो जाएगी।
पारिवारिक क़ानूनों का चौथा और महत्वपूर्ण हिस्सा वसीयत के आदेश एवं क़ानून का है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई नेक काम करना चाहता है, लेकिन मौक़ा नहीं मिलता। एक व्यक्ति को सर्वोच्च अल्लाह ने बड़े संसाधन दिए और बहुत दौलत दी। वह चाहता है कि कोई संस्था क़ायम कर दे, कोई वक़्फ़ क़ायम कर दे और ग़रीबों और नादारों की फ़लाह एवं बहबूद के लिए अपने जीवन में कुछ-न-कुछ कर जाए। जीवन में मन और शैतान बहकाते हैं और कभी-कभी इंसान कुछ कर नहीं कर पाता। मरने के क़रीब कुछ कर गुज़रने का भावना प्रभावी हो जाती है। अब इस मौक़े पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान के दिल में सन्तान और रिश्तेदारों के बारे में बद-गुमानियाँ पैदा हो जाती हैं। उदाहरणार्थ यही महसूस होने लगता है कि मेरे बुढ़ापे में मेरी इतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। मेरा अमुक काम नहीं किया। इंसान के दिमाग़ में एक-बार ये चीज़ें आ जाएँ तो शैतान उसको ग़लत रास्ते पर डाल देता है। बहुत-से लोगों में यह रुजहान पैदा हो जाता है कि वारिसों को विरासत से वंचित कर दें, disinherit कर दें जिसकी शरीअत में कोई गुंजाइश नहीं। यह जो अख़बारों में आता है कि मैंने ‘आक़’ (जायदाद से बेदख़ल) कर दिया, यह बिलकुल फ़ुज़ूल बात है। इसकी कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है। किसी को भी किसी हालत में किसी निश्चित वारिस को ‘आक़’ करने का अधिकार नहीं। शरीअत ने किसी को यह अनुमति नहीं दी कि जो हिस्सा अल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है या अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान किया है और इससे किसी को वंचित कर दिया जाए। कोई दस इश्तिहार दे या बीस इश्तिहार दे, इससे शरीअत का आदेश तो नहीं बदलता, अलबत्ता इश्तिहार देनेवाला आख़िरत में अपना मुँह काला होने का प्रबन्ध ज़रूर कर जाता है। पाकिस्तान के उच्च न्यायालयों ने कई बार तय कर दिया है कि इन इश्तिहारात की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी लोग ग़ुस्से में आकर अख़बारों में छाप देते हैं। व्यावहारिक रूप से शायद वंचित भी कर देते हों। बहरहाल यह गुंजाइश शरीअत ने रखी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई नेक काम करना चाहे तो अपने तरके के एक तिहाई की हद तक वह नेक काम के लिए ख़ास कर सकता है। दो तिहाई हिस्सा अनिवार्य रूप से उसके वारिस रिश्तेदारों को मिलेगा। एक तिहाई उस नेक काम का होगा जो वह करना चाहता है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वे ज़रूरतमन्द भी हैं और मुहताज भी हैं। लेकिन वे ज़रा दूर के रिश्तेदार हैं और अन्य वारिसों की मौजूदगी में उनको हिस्सा नहीं मिल सकता। शरीअत का एक उसूल यह भी है कि जो क़रीबी रिश्तेदार है इसको पहले मिलेगा और दूरवाले को नहीं मिलेगा। क़रीबी रिश्तेदार मौजूद न हों तो ज़्यादा दूरवाले को नहीं मिलेगा अलबत्ता कम दूरवाले रिश्तेदार को मिलेगा। मरनेवाले से जिसकी जितनी निकटता है उसके हिसाब से हिस्से नियुक्त हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। जितना आपका सम्बन्ध आपके दादा और दादी से होगा उतना सम्बन्ध पर दादा और पर दादी से नहीं हो सकता। जितना सम्बन्ध अपने सगे बहन-भाइयों से है वह दादा और परदादा की सन्तान से नहीं होगा। इस स्वाभाविक चीज़ का ध्यान रखते हुए शरीअत ने विरासत के आदेश दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई निकटवर्ती रिश्तेदार ज़रूरतमन्द और दरिद्र है और वह किसी अधिक निकटवर्ती रिश्तेदार की उपस्थिति की वजह से हिस्सेदार नहीं बन सकता, तो आप उसके लिए वसीयत कर दें। इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आप अपनी छोड़ी हुई धन-सम्पत्ति में से एक तिहाई के बारे में स्वयं ही कोई फ़ैसला कर दें। तीन में से एक हिस्सा।
ये इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों का चौथा बड़ा मैदान है। ये चार बड़े-बड़े विषय कुछ आंशिक मामलों के साथ, जिनका इन्हीं में से किसी-न-किसी विषय के साथ सम्बन्ध है, इस्लाम के पारिवारिक क़ानून का गठन करते हैं। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का दूसरा बड़ा हिस्सा है।
इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून
फ़िक़्हे-इस्लामी का तीसरा बड़ा हिस्सा वह है जिसको पश्चिमी क़ानून की शब्दावली में हम सिविल लॉ कह सकते हैं। यानी इस्लाम का दीवानी क़ानून। दीवानी क़ानून फ़िक़्हे-इस्लामी की शब्दावली में ‘फ़िक़्हुल-मुआमलात’ कहलाता है। ‘मुआमलात’ (मामलात) का शाब्दिक अर्थ तो dealing या ट्रांज़ेक्शंस है, लेकिन इस्तिलाही दृष्टि से मामलात से मुराद फ़िक़हे-इस्लामी का वह हिस्सा है जो दो या ज़्यादा व्यक्तियों के दरमियान लेन-देन और कारोबार के मामलात को जोड़ता है। यह लेन-देन एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के दरमियान हो रहा हो, या एक गिरोह और दूसरे गिरोह के दरमियान।
फ़िक़्हे-इस्लामी के इस हिस्से में लेन-देन के तमाम तरीक़ों पर चर्चा होती है, जिन चीज़ों का लेन-देन होगा उन चीज़ों का बयान, दौलत क्या है, इस्लाम में दौलत की परिकल्पना क्या है, दौलत की प्राप्ति कैसे होती है, दौलत का स्थानांतरण transfer कैसे होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दरमियान अक़्द या अनुबन्ध कैसे होता है। फ़िक़्हे-इस्लामी का यह हिस्सा एक समुद्र है, एक अथाह समुद्र है जो फ़िक़्हे-इस्लामी के नाम से हमारे सामने मौजूद है। चौदह सौ बरस से इसमें लगातार विकास हो रहा है। इसलिए कि कारोबार के नए-नए रूप अस्तित्व में आ रहे हैं। व्यापार की नई-नई समस्याएँ पैदा हो रही हैं। नए-नए आदेश रोज़ पैदा हो रहे हैं। पिछले पचास वर्षों में इस्लाम का जो व्यापार-क़ानून और व्यवहार-क़ानून अस्तित्व में आया है वह एक नए ढंग की व्यवस्था है। पूर्व तरीक़ों की उनमें निरन्तरता भी है और उनका अपना दूसरों से अलग होना भी है। बड़े अलग ढंग के गुण इस नए क़ानून में पाए जाते हैं। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का वह मैदान है जो उस समय तक लगातार फैलता रहेगा जब तक दुनिया में इंसान और मुसलमान रहेंगे, उनकी आवश्यताएँ पैदा होती जाएँगी और आदेश संकलित होते जाएँगे, यों इस फ़िक़्ही विभाग के नए-नए उप-विभाग बनते जाएँगे।
इन फ़िक़ही मामलों के कुछ ख़ास उप-विभागों का अगर बयान किया जाए तो वे दर्जनों हैं और अगर तमाम की गिनती की जाए तो वे दर्जनों से भी ज़्यादा हैं। उदाहरणार्थ ‘मुशारका’ और ‘मुज़ारबा’ इस्लाम के व्यापार-क़ानून का एक बहुत महत्वपूर्ण मैदान है, जो आज की धारणाओं एवं उर्फ़ और रिवाज के अनुसार कॉरपोरेट व्यापार और सामूहिक कारोबार का आधार बन रहा है। आजकल बैंकिंग की बात हो रही है। इस्लाम की बैंकिग-व्यवस्था पर संक्षिप्त-सी बात आगे चलकर करूँगा। इस्लामी बैंकिंग का सारा विकास ‘फ़िक़्हुल-मुआमलात’ ही के आदेश के आधार पर हो रहा है। फिर बैंकिंग में कई उप-विभाग हैं। धन की व्यवस्था है। शरीअत की रौशनी में ‘ज़र’ (धन) किसे कहते हैं। ‘ज़र’ के आदेश क्या हैं। ज़र के लेन-देन के नियम क्या हैं। जितना आप ग़ौर करते जाएँगे आपको एक तह में दूसरी तह और दूसरी में से तीसरी तह नज़र आती जाएगी। इसलिए कि इंसानी कर्म और इंसानी विचार और धारणाएँ असीमित हैं। उनके समाधान भी असीमित हैं। ये सब असीमित परतें इन्हीं चार हज़ार चार सौ स्पष्ट आदेशों से चीज़ें निकल रही हैं। इस स्रोत को देखें जो अब तक जारी है। दुनिया की हर किताब समाप्त हो जाती है, हर लेख पुराना हो जाता है। सौ-पचास वर्ष बाद उसमें जान नहीं रहती। जो कुछ उसमें से निकलना होता है वह निकल जाता है और फिर उसकी गणना प्राचीन अवशेषों में होने लगती है। क़ुरआन के ये स्पष्ट आदेश ऐसे हैं कि आज तक इससे समस्याएँ और आदेश निकलते चले आ रहे हैं।
इस्लाम के सामाजिक शिष्टाचार
मामलात की दो सतहें या दो प्रकार होते हैं। कुछ मामलात तो वे हैं जिनके परिणामस्वरूप कोई क़ानूनी हक़ या ज़िम्मेदारी अस्तित्व में आती है और कुछ मामलात वे हैं जिनसे कोई क़ानूनी अधिकार या कर्तव्य पैदा नहीं होते। पहले प्रकार के मामलों में क़ानूनी या अदालत से सम्पर्क हो सकता है, दूसरे प्रकार के मामलों में अदालत से सम्पर्क नहीं हो सकता। ये मामले व्यक्तियों के स्वयं करने के होते हैं।
मैं एक उदाहरण देकर बयान करता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आप अपना चश्मा मुझे बेच दीजिए और आप कहें कि पाँच सौ रुपये में ले लो। मैं पाँच सौ रुपये देने का वादा करके यह चश्मा आपसे लेकर चला जाऊँ तो यह एक क़ानूनी प्रकार का मामला होगा जिसमें दोनों पक्ष अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरणार्थ अगर मैं आपको वादे के अनुसार चश्मे की क़ीमत समय पर न चुकाऊँ, तो आपको जाकर अदालत में शिकायत करने का पूरा-पूरा हक़ प्राप्त है। आपकी शिकायत पर अदालत मुझे मजबूर करेगी कि मैं आपको आपके पैसे अदा कर दूँ। इसलिए कि शरीअत ने आदेश दिया है की जिसका जो हक़ है वह अदा करो। अगर कोई चीज़ ख़रीदो तो उसका मूल्य चुकाओ। यह मामलात का एक प्रकार है।
लेकिन जिस शरीअत ने यह आदेश दिया है कि मैं आपको आपका हक़ अदा कर दूँ, उसी शरीअत ने यह भी आदेश दिया है कि “जो व्यक्ति अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता हो उसको यह चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे।” (सहीह बुख़ारी, हदीस-6038) अब अगर आप मेरे घर में आएँ और मैं आपको खड़े-खड़े दरवाज़े ही से रुख़स्त कर दूँ और बड़े अक्खड़ या रूखे से लहजे में पूछूँ कि फ़रमाइए क्या बात है? आपको न बैठने का कहूँ न चाय-पानी का पूछूँ, तो आप यह कहने में बिलकुल सही होंगे कि यह तो बहुत ग़लत बात है। शरीअत ने कहा है कि मेहमान का सम्मान करो और मैंने इस आदेश के अनुसार आपका सम्मान नहीं किया और यों शरीअत के इस साफ़ और स्पष्ट आदेश का उल्लंघन किया। लेकिन अगर आप जाकर अदालत में इस रवैये की शिकायत करें तो अदालत आपकी यह शिकायत नहीं सुनेगी।
सारांश यह कि इंसानों के आपस के व्यवहार के दो प्रकार होते हैं। शरीअत ही ने दोनों का आदेश दिया है। एक प्रकार वह है जिसमें वे अधिकार और ज़िम्मादारियाँ पैदा होती हैं जो अदालतों के द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। दूसरे प्रकार के तहत वे अधिकार एवं कर्तव्य पैदा होते हैं जो अदालतों के द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं हैं। दूसरे को आप ‘फ़िक़्हे-तआमुले-इज्तिमाई’ या ‘फ़िक़्हे-मुआशरत’ कह सकते हैं। इस बात के आदेश कि इंसान जब आपस में सामाजिक रवैया अपनाएँ, एक-दूसरे के साथ सामाजिक रवैया रखें तो वे किन शिष्टाचारों के पाबन्द हों। ये सामाजिक शिष्टाचार फ़िक़्हे-इस्लामी का हिस्सा हैं। मेरे और आपके लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। कहीं वाजिब है, कहीं मुस्तहब और कहीं मंदूब है। यह सब दर्जे उनमें भी हैं। लेकिन इन मामलों में अदालत और राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। किसी अदालत को यह अधिकार नहीं कि वह यह आदेश दे कि लोग मिलने-जुलने में अमुक-अमुक सामाजिक शिष्टाचारों का अवश्य ही पालन करें। उदाहरणार्थ सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह कोई क़ानून बना दे ‘क़ानूने-मेहमान-नवाज़ी’। कल-कलाँ कोई साहब सत्ता के दंभ में कहने लगें कि चूँकि शरीअत ने मेहमान-नवाज़ी का आदेश दिया है तो सरकार यह क़ानून बना दे कि जब कोई मेहमान आए तो उसे चाय या ठंडा ज़रूर पिलाओ। ऐसी कोई चीज़ शरीअत की अपेक्षाओं में से नहीं है। शरीअत ने कहीं यह नहीं कहा कि आप इन शिष्टाचारों को क़ानून के ज़रिये लागू करें। ये वे चीज़ें हैं जो नैतिक आचरण से, प्रशिक्षण से, माहौल से पैदा होती हैं। फिर उनमें व्यक्तियों के दरमियान अन्तर होता है। शरीअत की व्यवस्था चूँकि अत्यन्त स्वाभाविक और नेचुरल है। मानव स्वभाव और मनोविज्ञान के अनुसार है। इसलिए जहाँ कम-से-कम से काम चल सकता हो वहाँ ज़्यादा-से-ज़्यादा पर कार्यान्वयन कराने में वह सख़्ती से काम नहीं लेती। जहाँ bare minimum को identify क्या जा सकता हो। यानी जहाँ शरीअत की अपेक्षाओं के bare minimum को identify क्या जा सकता हो, जहाँ किसी के अधिकार को quantify क्या जा सकता हो, वहाँ तो अदालतों को हस्तक्षेप करने का अधिकार शरीअत ने दिया है।
लेकिन जिन चीज़ों का सम्बन्ध इंसान के अपने subjective फ़ैसले पर हो, जहाँ अस्ल आदेश को quantify न किया जा सकता हो, जहाँ हर व्यक्ति अपने सब्जेक्टिव फ़ैसले से ही उसको quantify करता हो, वहाँ अदालतों को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च अल्लाह ने कुछ इंसान भी बनाए हैं, कुछ कम दानशील बनाए हैं, कुछ बहुत दानशील बनाए हैं और कुछ कंजूस और कुछ बहुत कंजूस बनाए हैं। अब उनमें से हर व्यक्ति मेहमान के सत्कार की अपनी परिकल्पना रखता है। आप यह नहीं कह सकते कि मेहमान के सत्कार के कम-से-कम अर्थ ये हैं। यह निर्धारण आसानी और क़तईयत के साथ नहीं हो सकता। मेहमान के सत्कार के हज़ारों अर्थ हो सकते हैं। और हर व्यक्ति अपनी समझ से जो अर्थ सही क़रार देगा उसके लिए वही अर्थ सही होगा। लेकिन चश्मे की क़ीमत के पाँच सौ रुपये quantifible चीज़ है। यह न पाँच सौ दस हो सकते हैं न चार-सौ नव्वे हो सकते हैं। चार-सौ नव्वे होंगे तो आपका हक़ प्रभावित होगा और पाँच-सौ दस होंगे तो मेरा हक़ प्रभावित होगा। “न तुम ज़ुल्म करो, न तुमपर ज़ुल्म किया जाए” (क़ुरआन, 2:279) जितना लिया है उतना ही दो। चूँकि इस आदेश पर अमल करना एक निश्चित अंदाज़ में सम्भव है इसलिए ये चीज़ें अदालतों के कार्य-क्षेत्र में हैं। जो चीज़ें गिनती में आने के योग्य नहीं हैं और subjective फ़ैसले पर आधारित हैं वे अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। वे इंसान स्वयं तय करें। अब आप देखें कि कितनी स्वाभाविक और नेचुरल बात है कि दोनों ही शरीअत के आदेश हैं। क़ियामत के दिन सर्वोच्च अल्लाह दोनों के बारे में पूछेगा। मेहमान के साथ तटस्थता का प्रदर्शन किया गया तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि अमुक आदमी तुम्हारे घर आया था, तुमने उसका उचित सत्कार क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हें उसके साथ इज़्ज़त से पेश आने का आदेश दिया गया था।
ये वे चार विभाग हैं यानी ‘फ़िक़्हुल-इबादात’, ‘फ़िक़्हुल-मनाकिहात’, ‘फ़िक़्हुल-मुआमलात’ और ‘फ़िक़्हुल-इज्तिमा’ या ‘फ़िक़्हे-मुआशरत’। अरबी में ‘मुआशरत’ नहीं कहते, बल्कि ‘इजतिमा’ कहते हैं। उर्दू में इजतिमा लोगों के जमा होने को कहते हैं, यह शब्दावली का अन्तर है। ‘फ़िक़्हे-मुआशरत’ को अंग्रेज़ी में ‘सोशल-फ़िक़्ह’ कह सकते हैं। ये चार विभाग फ़िक़्हे-इस्लामी के चार बड़े मौलिक मैदान बल्कि समुद्र हैं। उनमें आप ग़ोता लगाएँगे तो आपको लाखों मोती मिलेंगे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण की मैंने निशानदेही की है।
इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक कानून
पाँचवाँ विभाग वह है जिसको आजकल की शब्दावली में हम इस्लाम का इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून कह सकते हैं। इस्लामी शरीअत, पवित्र क़ुरआन और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो शिक्षा दी है वह मुस्लिम समुदाय की स्थापना की शिक्षा दी है। मुस्लिम समाज का गठन पवित्र क़ुरआन का पहला उद्देश्य है। पवित्र क़ुरआन का सबसे पहला सामूहिक लक्ष्य मुस्लिम समुदाय की स्थापना है। मुस्लिम समुदाय की ज़िम्मेदारियाँ अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्भाषायी हैं। पूरी दुनिया के सामने मुस्लिम समाज को सत्य की गवाही देने का आदेश दिया गया है। “और इसी प्रकार हमने तुम्हारे बीच एक उत्तम समुदाय बनाया है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो, और रसूल तुमपर गवाह हो।” (क़ुरआन, 2:143) इसलिए मुस्लिम समाज का एक विश्वव्यापी चरित्र, एक वैश्विक ज़िम्मेदारी और एक अन्तर्भाषायी कर्तव्य पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह बयान हुआ है। इस चरित्र को निभाने के लिए मुस्लिम समाज की एकता और रक्षा ज़रूरी है। इन महान वैश्विक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुस्लिम समाज को संसाधन दरकार हैं। इन संसाधनों में से एक संसाधन हुकूमत और राज्य भी है। जब तक राज्य और हुकूमत की ताक़त उपलब्ध नहीं होगी, मुस्लिम समाज बहुत-से सामूहिक और सामाजिक कार्य नहीं कर सकेगा। इसी प्वाइंट की तरफ़ इशारा करते हुए हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि “निस्सन्देह सर्वोच्च अल्लाह राज्य के द्वारा ऐसे काम लेता है जो क़ुरआन के द्वारा नहीं हो सकते।” सर्वोच्च अल्लाह बहुत-सी चीज़ें जो रोकने की हैं वह हुकूमती सत्ता के ज़रिये रोकता है और पवित्र क़ुरआन के ज़रिये नहीं रोकता। पवित्र क़ुरआन ज़ेहन बनाने और प्रशिक्षण के लिए है। लेकिन अगर कोई इतना बदनसीब हो कि उसकी ज़ेहन साज़ी ही न हो, इतना दुष्चरित्र हो कि उसका चरित्र निर्माण ही न हो सके तो वहाँ पर शरीअत के आदेशों के राज्यकीय भाग पर अमल कराने और व्यक्तिगत भागों पर अमल के संसाधन, और माहौल पैदा करने में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार और सत्ता से भी काम लिया जाएगा। पवित्र क़ुरआन प्रशिक्षण देता है कि एक-दूसरे की जान-माल की रक्षा करो। एक इंसान की जान को तमाम मानवता की जान समझो। लोगों के माल और सम्पत्ति को अपने माल और सम्पत्ति की तरह महत्वपूर्ण और पवित्र समझो। लेकिन यह प्रशिक्षण कोई प्राप्त न करे और लोगों की जान-माल को नुक़्सान पहुँचाए तो इसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि पवित्र क़ुरआन में क़त्ल, चोरी और दूसरे अपराधों की सज़ा का उल्लेख मौजूद है। अब सवाल यह है कि यह सज़ा कौन देगा? व्यक्तियों को तो यह अधिकार नहीं कि क़ानून अपने हाथ में लेकर कार्रवाई करें, किसी व्यक्ति को तो यह अधिकार नहीं कि फ़ौजदारी क़ानून को अपने हाथ में ले और चोर का हाथ काट दे। यह तो हुकूमतों के करने का काम है।
गोया पवित्र क़ुरआन के कुछ आदेश वे हैं जिनपर कार्यान्वयन के लिए हुकूमत और राज्य का होना ज़रूरी है। हुकूमत होगी तो उन आदेशों का पालन होगा। हुकूमत नहीं होगी तो शरीअत के बहुत-से आदेशों का पालन नहीं हो सकेगा। जब इन आदेशों का पालन नहीं होगा तो उन आदेशों के फल एवं बरकतों से मुस्लिम समाज भी वंचित रहेगा और शेष मानवता भी इस्लामी जीवन व्यवस्था का व्यावहारिक नमूना बड़ी हद तक न देख सकेगी। इसके अलावा जब शरीअत के आदेशों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का पालन नहीं होगा तो जिस तरह का प्रशिक्षण पवित्र क़ुरआन करना चाहता है वह प्रशिक्षण पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं आएगा। जब यह प्रशिक्षण व्यवहार में नहीं आएगा तो मुस्लिम समाज में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएँगी। मुस्लिम समाज में ख़राबियाँ पैदा होंगी तो पवित्र क़ुरआन के लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए उम्मत को एक माध्यम और एक ज़रिये के तौर पर आवश्यकता है कि इसका एक राज्य भी हो। राज्य जब बनेगा तो उसका क़ानून भी होगा। उसकी एक व्यवस्था होगी, मार्गदर्शन और आदेश होंगे, मौलिक धारणाएँ होंगी। नियम-क़ानून यानी इस्लाम के संवैधानिक आदेशों पर एक दिन पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। यह जो नियम-क़ानून हैं उनके लिए इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने दो शब्दावलियाँ प्रयुक्त की हैं, ‘सियासते-शरईया’, या ‘अहकामे-सुल्तानिया’। कुछ लोगों ने ‘सियासते-शरईया’ के नाम से किताबें लिखी हैं, कुछ ने ‘अहकामे-सुल्तानिया’ के नाम से लिखी हैं।
अल्लामा क़ाज़ी अबुल हसन मावरदी जो प्रसिद्ध शाफ़िई फ़क़ीह हैं। उनकी किताब ‘अहकामे-सुल्तानिया’ के नाम से प्रसिद्ध है और इसका उर्दू अनुवाद भी मिलता है। अल्लामा इब्ने-तैमिया की एक प्रसिद्ध किताब ‘सियासते-शरईया’ के नाम से है। इस प्रकार में यही समस्याएँ चर्चा में आई हैं कि इस्लामी राज्य के मौलिक अधिकार क्या हैं और राज्य की संस्था को कैसे अस्तित्व में लाया जाए और कैसे संकलित किया जाए।
इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून
फ़िक़्हे-इस्लामी का छटा बड़ा हिस्सा ‘जिनायात’, यानी इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून है। जहाँ इंसान होंगे वहाँ ग़लतियाँ भी होंगी। ग़लतियों से सौ प्रतिशत पाक और मुक्त कोई समाज नहीं होता। सर्वोच्च अल्लाह ने इंसान में ऐसी भावनाएँ और प्रवृत्तियाँ रखी हैं कि वह ग़लती करता है। “तुममें से हर एक ग़लती करनेवाला है। ग़लती करनेवालों में बेहतरीन वह है जो तौबा करता हो।” लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तौबा न करते हों और समाज में खुल्लम-खुल्ला अपराध करते हों। उनके लिए एक क़ानून होना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि क्या चीज़ अपराध है और अगर कोई चीज़ अपराध है तो उसकी सज़ा क्या है। इस मामले में शरीअत ने एक बहुत ही विस्तृत दिशानिर्देश दिया है जिसपर आगे चलकर विस्तृत चर्चा होगी। यह एक अत्यन्त सम्बद्ध, अत्यन्त संगठित और अत्यन्त सन्तुलित व्यवस्था है जिसमें अपराध और सज़ा की मौलिक धारणाएँ एवं आदेश दिए गए हैं कि किस अपराध की क्या सज़ा होगी, किन हालात में और किस तरह सज़ा दी जाएगी, कितनी सज़ा दी जाएगी, कौन सज़ा देगा, उसके परिणाम अगर कुछ हैं तो उनसे कैसे निबटा जाएगा। यह शरीअत का छटा मौलिक भाग है, जिसको ‘फ़िक़्हुल-जिनायात’ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि यह इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून यानी Criminal law of Islam है।
जब यह बात तय हो गई कि समाज में कई लोग अपराध करते हैं और हर दौर में करते रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सज़ाओं का होना भी ज़रूरी है। अत: यह तय करना भी ज़रूरी है कि सज़ा कैसे दी जाएगी। मुजरिम के मुजरिम होने का फ़ैसला कौन करेगा। क़ानून को तोड़नेवालों से कौन निबटेगा। क़ानूने-शरीअत, ख़ास तौर पर ‘फ़िक़्हुल-जिनायात’ के कुछ आदेशों के सिलसिले में यह निर्धारण करना भी ज़रूरी होता है कि ये अपराधियों पर कैसे फ़िट होंगे। कुछ कर्मों के बारे में यह निर्धारण करना भी ज़रूरी है कि यह अपराध हैं। यह तय करना भी ज़रूरी है कि अपराधियों को सज़ा कैसे दी जाए। मुजरिम के मुजरिम होने का निर्धारण कैसे किया जाए, कौन यह निर्धारण करेगा। सज़ा कैसे दी जाए, सज़ा लागू कैसे हो। यह वह विभाग है जिसको क़ानूने-ज़ाब्ता यानी Procedural law of Islam कहते हैं। यह इस्लामी क़ानून का वह विभाग है जिसको ‘अदबुल-क़ाज़ी’ कहते हैं। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का सातवाँ बड़ा विभाग है और इसपर अभी और बात होगी।
इस्लाम का अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून
फ़िक़्हे-इस्लामी का आठवाँ बड़ा भाग वह है जो मुसलमानों के सम्बन्ध को दूसरी क़ौमों के साथ जोड़ता है। दूसरी क़ौमों के साथ मुसलमानों के सम्बन्ध कैसे जोड़े जाएँ। यह इस्लामी क़ानून का वह विभाग है जिसको आप इस्लाम का अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून Muslim International law of Islam या International Law कह सकते हैं।
फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की शब्दावली में यह विभाग ‘सियर’ कहलाता है। सियर, सीरत का बहुवचन है। ‘सीरत’ के शाब्दिक अर्थ हैं कार्य-नीति और रवैया। ‘सियर’ के शाब्दिक अर्थ होंगे रवैये या कार्य-नीतियाँ। शब्दावली में ‘सियर’ से मुराद मुसलमानों की वह कार्य-नीति और रवैया है जो ग़ैर-मुस्लिमों के साथ वे अपने सम्पर्क और सम्बन्ध में अपनाते हों। इस तरह आगे चलकर ‘सियर’ का अर्थ उस नियमों एवं आदेशों के संग्रह का हो गया जो मुसलमानों और दूसरों के बीच सम्पर्क और ग़ैर-मुस्लिमों से इस्लामी राज्य के सम्बन्ध को संकलित और संगठित करता हो। ग़ैर-मुस्लिमों में वे ग़ैर-मुस्लिम भी शामिल हैं जो दारुस्सलाम यानी मुसलमानों के देश से बाहर रहते हैं, और वे ग़ैर-मुस्लिम भी शामिल हैं जो मुसलमानों के देश में रहते हैं।
दुनिया के लोगों के साथ मुसलमानों के सम्बन्ध कैसे हों, इन सम्बन्धों की तीन शक्लें हो सकती हैं। या तो मुसलमान उनमें किसी के ख़िलाफ़ युद्धरत होंगे, या शान्तिपूर्ण स्थिति में होंगे और दोस्ती होगी या तटस्थ होंगे। इसके अलावा कोई शक्ल नहीं हो सकती। या आप किसी के साथ युद्ध की हालत में होंगे, या शान्ति की स्थिति में होंगे, या निरपेक्ष होंगे। ‘सियर’ के ज्ञान में इन तीनों विभागों के बारे में बात की गई है और इन तीनों प्रकार के सम्पर्कों और सम्बन्धों के आदेश बयान किए गए हैं। पवित्र क़ुरआन में मौलिक निर्देश मौजूद हैं। इन निर्देशों का बड़ा हिस्सा सूरा-8 अनफ़ाल और सूरा-9 तौबा में दिया गया है। कुछ आदेश सूरा-2 बक़रा में हैं और कुछ सूरा-47 मुहम्मद में आए हैं। शेष सूरतों में भी कुछ अलग-अलग आदेश आए हैं। लेकिन ज़्यादा-तर सूरा-8 अनफ़ाल, सूरा-9 तौबा, और कुछ आदेश सूरा-47 मुहम्मद में हैं।
हदीसों में और अधिक विवरण आए हैं। और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसको एक बिलकुल अलग ज्ञान-विभाग के तौर पर संकलित किया है। यहाँ यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) क़ानून और मानवता के इतिहास में वे लोग हैं जिन्होंने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को क़ानून के एक अलग विभाग के रूप में दुनिया में परिचित कराया। दूसरी सदी हिजरी के इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) से पहले दुनिया इस विचार से परिचित नहीं थी कि क़ानून के दो हिस्से होने चाहिएँ। एक राष्ट्रीय क़ानून municipal law कहलाया और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून Interantioanal law कहलाया जो मुल्कों और क़ौमों के दरमियान सम्बन्ध को स्थापित करे। पश्चिमी दुनिया में जिस व्यक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर सबसे पहली किताब लिखी, जिसको वहाँ Father of International Law यानी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का जनक कहा जाता है, उसका नाम Hugo Grotius था। ह्यूगो ग्रोशियस ने 1640 ई॰ में यानी लगभग ग्यारहवीं सदी हिजरी में एक किताब लिखी थी जो Law of War and Peace के नाम से मौजूद है। अस्ल किताब तो डच भाषा में थी, लेकिन बाद में फ़्रेंच, जर्मन, अंग्रेज़ी और उर्दू भाषाओं में इसके अनुवाद हुए, जो अब आम तौर पर उपलब्ध हैं। इससे पहले किसी पश्चिमी भाषा में कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं थी जिसको अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की किताब क़रार दिया जा सके, और इस विषय पर विधिवत रूप से एक लेख के तौर पर कहा जा सके कि यह किताब जंग, सुलह (सन्धि) या क़ौमों के दरमियान सम्बन्धों के क़ानूनों पर लिखी गई है। इस तरह की कोई किताब पश्चिमी जगत् में ह्यूगो ग्रोशियस से पहले मौजूद नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसको अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का जनक क़रार दिया, लेकिन वास्तव में उनके ज्ञान में यह बात नहीं आई कि ह्यूगो ग्रोशियस के जन्म से 860 वर्ष पहले इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के विषय पर एक दर्जन किताबें लिख दी थीं।
सबसे पहला व्यक्तित्व जिसने अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर कोई विधिवत किताब लिखी वह इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) हैं। उनकी किताब का नाम ‘किताबे-सियर अबी-हनीफ़ा’ था। यानी वह किताबे-सियर जो अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने लिखी। उनसे पहले दुनिया के इतिहास में किसी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के आदेशों पर कोई विधिवत किताब नहीं लिखी थी। अफ़सोस है कि यह किताब हम तक पहुँच नहीं सकी और कहीं नष्ट हो गई है। इस विषय पर जो प्राचीनतम किताबें हम तक पहुँची हैं, वे इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के शागिर्द इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी की तीन किताबें हैं। एक किताब है ‘किताबुस-सियर अस-सग़ीर’। यह बड़ी संक्षिप्त किताब है और संभवतः छात्रों के लिए लिखी गई थी। यह किताब आज हमारे पास अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ मौजूद है। फ़्रांसीसी और तुर्की भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है और यह किताब आज भी उपलब्ध है। इस किताब के बाद इमाम मुहम्मद को ख़याल हुआ कि यह बहुत संक्षिप्त है, एक विस्तृत किताब भी होनी चाहिए। इसपर उन्होंने एक विस्तृत किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने ‘किताबुस-सियर अल-कबीर’ रखा, यानी बड़ी किताब या Major Book on International Law. यह किताब जब इमाम मुहम्मद ने लिखी तो मुस्लिम जगत् में इसका असाधारण स्वागत किया गया। इस किताब के पूर्ण होने के मौक़े पर बड़ा जश्न मनाया गया। इसलिए कि इस विषय पर पहली बार इतनी मोटी और विस्तृत किताब लिखी गई थी। जिस दिन यह किताब पूरी हुई उस दिन पूरे बग़दाद में इसकी ख़ुशियाँ मनाई गईं। ख़लीफ़ा हारून रशीद ने स्वयं भी इस जश्न में हिस्सा लिया। इमाम मुहम्मद के घर से सरकारी तौर पर एक जुलूस निकाला गया जिसमें इस किताब के भाग रखे गए और लोग इस किताब को लेकर जुलूस के रूप में ख़लीफ़ा के यहाँ गए और इमाम मुहम्मद ने यह किताब हारून रशीद को पेश की। हारून ने इस मौक़े पर कहा कि मेरे शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण कारनामा अस्तित्व में आया है वह किसी शहर और किसी इलाक़े की फ़त्ह या कोई और चीज़ नहीं, बल्कि इस किताब की रचना है। ख़लीफ़ा ने कहा कि यह अति महत्वपूर्ण कारनामा है जो सर्वोच्च अल्लाह की नियति से मेरे ज़माने में पूरा हुआ।
यह किताब बहुत मोटी थी। इमाम मुहम्मद को ख़याल हुआ कि एक दरमियाने दर्जे की किताब भी लिखें। उन्होंने एक तीसरी किताब ‘किताबुस-सियर अल-वसीत’ यानी ‘दरमियानी किताबे-सियर’ लिखी। यह किताब अधूरे रूप में मख़तूता (पाँडुलिपि) की हैसियत से इस्तंबोल (तुर्की) के पुस्तकालय सुलैमानिया में मौजूद है। उन्होंने यह किताब पूरी की थी या नहीं, यह मालूम नहीं, लेकिन जो प्रति आज पुस्तकालय सुलैमानिया में मौजूद है वह अधूरी है और उसपर लिखा हुआ है ہٰذا آخرماالفہ محمد ابن الحسن “यह वह आख़िरी किताब है जो इमाम मुहम्मद-बिन-हसन (यानी इमाम शैबानी) ने संकलित की है।”
इमाम मुहम्मद के ज़माने में और कई लोगों ने भी इस विषय पर किताबें लिखीं। उनमें कम-से-कम छः किताबें आज हमारे पास छपी हुई मौजूद हैं। मेरे निजी पुस्तकालय में भी हैं। ये सब किताबें दूसरी सदी हिजरी में लिखी गई थीं। अत: यह कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का जनक अमुक डच या कोई और क़ानूनविद् है, दुरुस्त नहीं है। तथ्यों की दृष्टि से यह बात ग़लत है। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का अगर कोई व्यक्ति जनक हो सकता है तो या तो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) हो सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस विषय पर एक विधिवत किताब लिखी या फिर इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी हैं जिनकी लिखी हुई किताबें आज मौजूद हैं।
ये फ़िक़्हे-इस्लामी के आठ बड़े-बड़े विभाग हैं जिनपर अलग-अलग किताबें मौजूद हैं। उनमें से पहले चार विभाग यानी इबादात, मनाकिहात, मुआमलात और फ़िक़्हे-मुआशरत वे विभाग हैं जो क़ानून की शब्दावली में Personal Jurisdiction रखते हैं। क़ानूनों के लागू होने का एक तो कार्य-क्षेत्र व्यक्ति होता है। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति यानी मैं, आप या कोई और इस क़ानून का पाबंद हो। यह व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र कहलाता है। दूसरा Territorial Jurisdiciton या इलाक़ाई कार्य-क्षेत्र कहलाता है। किसी ख़ास इलाक़े में इस क़ानून पर अमल होगा उस इलाक़े से बाहर अमल नहीं होगा। इनमें जो पहले चार हैं वे व्यक्तिगत कार्य-क्षेत्र रखते हैं और मुसलमान जहाँ भी है उनपर अमल करेगा। मैंने बताया था कि अगर कल यह साबित हो जाए कि मिर्रीख़ पर इंसानी आबादी मौजूद है। वहाँ प्लाट तक़सीम होने लगें और आप वहाँ जाकर घर बना लें तो आपको मिर्रीख़ पर भी इन आदेशों पर अमल करना पड़ेगा। इसका उसूल यह है कि “मुसलमान जहाँ भी होगा इन चार मैदानों में इस्लाम के आदेशों का पाबंद होगा।” शेष चार यानी ‘अहकामे-सुल्तानिया’ या ‘सियासते-शरईया’, फ़िक़्हुल-जिनायात’, ‘अदबुल-क़ाज़ी’ और ‘सियर’ वे हैं जिनका कार्य-क्षेत्र इलाक़ाई है, इस अर्थ में कि इस्लामी राज्य की सीमाओं में इस्लामी हुकूमत इन अध्यायों के आदेशों पर अमल करेगी। इस्लामी राज्य इन आदेशों पर अमल कराने में सक्षम है। व्यक्ति सीधे-सीधे इन आदेशों पर अमल करने में सक्षम नहीं हैं। व्यक्तियों से यह नहीं कहा गया कि तुम क़त्ल और अन्य अपराधों की सज़ाएँ ख़ुद ही लोगों को दिया करो। व्यक्तियों से यह नहीं कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर अमल करो। व्यक्ति उन निर्देशों के पाबंद हैं जो इबादात, मनाकिहात, मुआमलात, फ़िक़्हे-इज्तिमाई के अध्यायों में बयान हुए हैं। चोर को सज़ा कैसे दी जाए, अदालतें कैसे क़ायम की जाएँ, जज कैसे नियुक्त किए जाएँ, टैक्स कैसे लगाए जाएँ, ये काम व्यक्तियों के नहीं, बल्कि हुकूमतों के करने के हैं। इसलिए फ़िक़्हे-इस्लामी और क़ानून में एक बड़ा मौलिक अन्तर है। वह अन्तर यह है कि उनके यहाँ क़ानून उसको कहते हैं जो अदालतों के ज़रिये सरकार की स्वीकृति से लागू हो। हमारे यहाँ फ़िक़्ह उसको कहते हैं जिसमें जीवन के सभी कार्य-क्षेत्र आते हों। जिसमें सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। जिसमें निजी और सामूहिक जीवन के दोनों पहलू शामिल हैं।
इस्लामी क़ानून संहिता
यह तो फ़िक़्हे-इस्लामी के आठ बड़े-बड़े विभाग हैं। उनके अन्दर उप विभागों पर अगर हम आएँ तो वे इतने विस्तृत हैं कि उनमें से किसी एक का भी पूरा विवरण बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन समझने की ख़ातिर मैं उदाहरण के रूप में एक-दो का उल्लेख करता हूँ।
अभी मैंने उल्लेख किया था कि ‘अदबुल-क़ाज़ी’ फ़िक़्हे-इस्लामी का सातवाँ महत्वपूर्ण विभाग है। अदबुल-क़ाज़ी का शाब्दिक अर्थ तो है, क़ाज़ी (न्यायाधीश) के शिष्टाचार, क़ाज़ी के लिए निर्देशन या अदालत की कार्य-प्रणाली, लेकिन पारिभाषिक दृष्टि से ‘अदबुल-क़ाज़ी’ इस्लाम की क़ानून संहिता को कहते हैं। इस्लाम की क़ानून संहिता या Islamic law of procedure परिभाषा में ‘अदबुल-क़ाज़ी’ कहलाता है। इस क़ानून का संकलन इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने दूसरी सदी हिजरी ही में शुरू कर दिया था। पहली सदी हिजरी के अन्त में ‘अदबुल-क़ाज़ी’ की शब्दावली इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने दी थी। दूसरी सदी हिजरी से किताबों में ‘अदबुल-क़ाज़ी’ की शब्दावली मौजूद है। इमाम मालिक (रह॰) की मुवत्ता में ‘अदबुल-क़ाज़ी’ की शब्दावली मौजूद है। उनके समकालीन इस्लामी विद्वानों की किताबों में यह शब्दावली मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने पहली सदी हिजरी के अन्त तक यह तय कर दिया था कि क़ानून के बड़े-बड़े विभाग दो हैं। एक विभाग वह है जिसको आजकल की शब्दावली में क़ानूने-अस्ली यानी substantive law कहा जाता है। दूसरा विभाग वह है जिसको क़ानून संहिता यानी procedural law कहा जाता है।
आज दुनिया के हर क़ानून के दो विभाग होते हैं। एक विभाग वह है जो क़ानून में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को तय करता हो। दूसरा विभाग वह है जो इन अधाकारों और कर्तव्यों पर अमल कराने के रास्ते या तरीक़े को प्रस्तावित करता हो। दुनिया लगभग दो हज़ार वर्ष तक क़ानून संहिता की परिकल्पना से परिचित नहीं थी। हम्मूराबी के क़ानून में क़ानूने-अस्ली और क़ानून संहिता की कोई परिकल्पना नहीं मिलती। रोमन लॉ, यहूदी क़ानून, मनुशास्त्र (मनुस्मृति), जसटीनियन के कोड में यह अन्तर नहीं मिलता। उनसे पहले संकलित क़ानूनों के जितने और जो भी नमूने उपलब्ध हैं उनमें ऐसी कोई परिकल्पना मौजूद नहीं है। उनके यहाँ क़ानून एक ही था, जिसमें क़ानूने-अस्ली और क़ानून संहिता मिले-जुले थे और इन दोनों में कोई अन्तर नहीं था। एक ही धारा में एक वाक्य अस्ली क़ानून के बारे में होता तो दूसरा वाक्य संहिता के क़ानून के बारे में होता था। उनके ज़ेहन में यह अन्तर पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इस अन्तर को समझा ही नहीं। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इस अन्तर को पहली सदी में ही समझ लिया था।
‘अदबुल-क़ाज़ी’ के विषय पर सबसे पहली किताब लिखने का सौभाग्य इमाम अबू-यूसुफ़ को प्राप्त हुआ। इमाम अबू-यूसुफ़ जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) में बड़ा ऊँचा स्थान रखते हैं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के सबसे पहले शागिर्द हैं। इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) दो कलाओं के अविष्कारक हैं। एक ‘अदबुल-क़ाज़ी’ जिसपर उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी, दूसरा ‘क़ानूने-मालियाते-आम्मा’। वह इस्लामी राज्य के पहले चीफ़ जस्टिस थे। अब्बासी साम्राज्य में उनको चीफ़ जस्टिस नियुक्त किया गया। उन्होंने ‘महकमा-ए-क़ज़ा’ (न्यायिक विभाग) को संगठित किया। क़ाज़ियों (न्यायाधीशों) की नियुक्ति की, उनका प्रशिक्षण किया, उनको निर्देश दिए और उनका मार्गदर्शन किया। इस पूरे अनुभव की रौशनी में मानव इतिहास में पहली बार उन्होंने क़ानून संहिता पर एक अलग किताब लिखी। अगरचे यह किताब हम तक पहुँची नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और जीवनी-लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। कुछ वृतान्त लेखकों के लेखों से मालूम होता है कि यह किताब छठी सदी हिजरी तक उपलब्ध थी। कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्याएँ भी लिखी थीं। ये व्याख्याएँ भी बाद की कई सदियों तक जानी-मानी रहीं।
जो प्राचीनतम पुस्तक हम तक पहुँची है, जो आज क़ानून संहिता पर लिखी जानेवाली प्राचीनतम पुस्तक है वह इमाम अबू-बक्र ख़स्साफ़ ने लिखी है जिनका देहान्त 260 हि॰ में हुआ था। गोया तीसरी सदी हिजरी में उन्होंने यह किताब लिखी थी। यह किताब आज भी मौजूद है, अत: हम कह सकते हैं कि तीसरी सदी हिजरी से इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘अदबुल-क़ाज़ी’ के नाम से एक संकलित कला दुनिया को दी। वह कला जिसको इमाम अबू-बक्र ख़स्साफ़ ने अलग किताब के रूप में संकलित करके हमारे लिए छोड़ा। इमाम ख़स्साफ़ की यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई। पूरे मुस्लिम जगत् के छात्रों और विद्वानों ने इसको हाथों-हाथ लिया। इसकी शरहें (व्याख्याएँ) लिखी गईं। इन शरहों में से एक व्याख्या जो किताब के लिखे जाने के लगभग एक सौ वर्ष बाद लिखी गई, वे चार भागों में है और इसका नाम ‘शरहे-अदबुल-क़ज़ा’ है। यह इमाम उमर-बिन-माज़ा की लिखी हुई है। इस व्याख्या का उर्दू अनुवाद मौजूद है जो अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। यह उर्दू भाषा में क़ानून संहिता की प्राचीनतम पुस्तक का अनुवाद है। उर्दू भाषा उस समय पैदा ही नहीं हुई थीं, जब यह किताब लिखी जा रही थी। इसी तरह अंग्रेज़ी भाषा भी वर्तमान रूप में मौजूद नहीं थी जब यह किताब लिखी गई थी। धरती पर क़ानून संहिता पर कोई किताब तो क्या होती, क़ानून जगत् में इस विषय या ज्ञान-विभाग की कोई धारणा तक मौजूद नहीं थी। पश्चिम में यह धारणा भी नई है। पिछले दो-ढाई सौ वर्ष में आई है। इससे पहले क़ानून का एक ही विभाग था जिसमें substansive और procedural दोनों प्रकार के क़ानून मिले-जुले थे।
अभी मैंने बताया कि उनमें से बहुत-से विभागों के उप विभाग अनगिनत हैं। जिनको अलग-अलग ज्ञान-विज्ञान के तौर पर फ़ुक़हा ने संकलित किया। उनमें से भी एक-दो का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ।
इस्लाम का दीवानी क़ानून या ‘फ़िक़्हुल-मुआमलात’
जैसा कि बयान किया जा चुका है कि फ़िक़्हे-इस्लामी का सबसे बड़ा विभाग मामलात का है जिसको इस्लाम का दीवानी क़ानून या सिवल लॉ कहा जा सकता है? इस्लाम का यह दीवानी क़ानून हज़ारों विषयों और लाखों समस्याओं एवं आदेशों से बहस करता है। इन बहुत-से विषयों में से एक यह भी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई लेन-देन या मामला करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। वह मामला क्या माल के आधार पर होगा। अगर माल के आधार पर होगा तो माल किसे कहते हैं, उसकी कितनी क़िस्में हैं, माल प्राप्त कैसे होता है, स्थानांतरित कैसे होता है, ये सारी चीज़ें दौलत (Wealth) से सम्बन्धित हैं। आज पश्चिमी दुनिया यह दावा करते नहीं थकती कि एडम स्मिथ (Adam Smith) पहला आदमी था जिसने दौलत के विषय पर किताब ‘Wealth of Nations’ लिखी। ठीक है, पश्चिम में वह पहला आदमी होगा जिसने दौलत पर किताब लिखी होगी। पश्चिमवाले जिस चीज़ को नहीं जानते उसके अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं। वे अपने-आपको जानते हैं तो वे अपने को ही पूरी दुनिया समझते हैं।
जब मैं बचपन में मैट्रिक या एफ़॰ए॰ की किताबें पढ़ता था, तो उसमें लिखा होता था कि भारत की खोज अमुक सन् में हुई। तो मुझे हैरत होती थी कि यहाँ के लोगों ने कैसे अपने ही देश को खोज लिया। मैं सोचता था कि मैं स्वयं इस इलाक़े का रहनेवाला हूँ जिसको भारत कहते थे। अब उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बंगला देश शामिल हैं। तो मैं अपने-आपको कैसे खोज सकता हूँ। मैं अपने बारे में क्यों कहूँ कि मैं अमुक सन् में खोजा गया। मेरा इलाक़ा तो हज़ारों वर्ष से मौजूद है। इस्लाम से पहले भी यह मौजूद था और इस समय भी यहाँ इंसान बसते थे। यह बात मुझे अजीब सी लगती थी। बाद में यह बात मेरी समझ में आई कि जो लोग इस इलाक़े के अस्तित्व से अनजान थे उनके लिए यह कोई नई खोज हुई होगी। हमारे लिए तो यह कोई नई खोज नहीं थी। उसी मानसिकता की वजह से वह जिस चीज़ से अपरिचित होते हैं उसको समझते हैं कि पूरी दुनिया इससे अपरिचित होगी और इस चीज़ के लिए वह शब्दावली प्रयुक्त करते हैं जो एक नौ-सिखिया प्रयुक्त करता है।
इसलिए अगर वे यह कहते हैं कि Wealth of Nations दुनिया के इतिहास में वित्त के विषय पर लिखी जानेवाली पहली किताब थी तो उन्हें शायद यह अधिकार है कि वे ऐसा कहें, कि अपरिचित आदमी ऐसी ही बातें किया करता है। लेकिन आज दूसरी सदी की लिखी हुई कम-से-कम तीन किताबें वित्त पर लिखी हुई मौजूद हैं। अबू-उबैद क़ासिम-बिन-सलाम की किताब ‘किताबुल-अमवाल’ है। उनका सम्बन्ध दूसरी सदी हिजरी से था। इस किताब का उर्दू अनुवाद भी अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने किया है। यह अनुवाद दो मोटे भागों में उपलब्ध है। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी मिलता है। दूसरी किताब इमाम यह्या-बिन-आदम की ‘किताबुल-ख़िराज’ है। तीसरी किताब इमाम अबू-यूसुफ़ की ‘किताबुल-ख़िराज’ है। इमाम अबू-उबैद की किताब में यह बताया गया है कि दौलत किस चीज़ को कहते हैं, उसकी क़िस्में कितनी हैं, उसका तरीक़ा क्या है और कहाँ से आती है। यह एक अलग कला है जिसपर पश्चिम में भी बहुत बाद में किताबें लिखी गई हैं।
जब दौलत पर चिन्तन-मनन किया जाएगा तो ‘मालियाते-आम्मा’ (सार्वजनिक वित्त) की बहस पैदा होगी। इसलिए कि व्यक्तियों की दौलत का अर्थ और है, क़ौमों की दौलत का अर्थ और है। आपके पास अगर अल्लाह की दी हुई दौलत है तो उसका इस्तेमाल भी और है और आने का रास्ता भी और है और इसके आदेश भी और हैं। लेकिन अगर सरकार के ख़ज़ाने में पैसे रखे हुए हैं तो उसके आने के तरीक़े भी अलग होंगे और ख़र्च के तरीक़े भी अलग होंगे। उस के आदेश भी और होंगे। तो गोया दौलत की एक ख़ास क़िस्म हो गई जिसको आप राज्य या सरकारी दौलत कह सकते हैं। यह एक अलग कला है जिसको Public Finance कहते हैं। गोया एक आम फ़ाइनांस होता है और एक पब्लिक फ़ाइनांस है। पब्लिक फ़ाइनांस पर मानव इतिहास में सबसे पहली किताब इमाम अबू-यूसुफ़ ने लिखी जिसका नाम ‘किताबुल-ख़िराज’ है और आज हमारे पास मौजूद है। इसका अनुवाद अंग्रेज़ी, उर्दू और दुनिया की कई दूसरी भाषाओं में मौजूद है।
‘अदबुल-क़ाज़ी’ की अन्तर्वस्तुएँ
दूसरा महत्वपूर्ण क़ानूनी विभाग या ज्ञान जिस पर इमाम अबू-यूसुफ़ ने सबसे पहले किताब लिखी और बाद में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इस कला को आगे बढ़ाया वह जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, ‘अदबुल-क़ाज़ी’ कहलाता है। ‘अदबुल-क़ाज़ी’ के नाम से आज बहुत-सी छोटी-बड़ी किताबें मौजूद हैं। उर्दू में भी ‘अदबुल-क़ाज़ी’ पर किताबें मौजूद हैं, अरबी में भी बड़ी संख्या में किताबें क़रीब-क़रीब हर सदी में लिखी हुई मौजूद हैं। प्रकाशित भी और हस्तलिखित पाँडुलिपियों के रूप में भी। फ़ारसी, तुर्की और दूसरी भाषाओं में भी हैं। एक-आध किताब अंग्रेज़ी में भी है। लेकिन अस्ल और मौलिक संग्रह अरबी में ही है।
‘अदबुल-क़ाज़ी’ पर लिखी जानेवाली इन किताबों की समाग्री का जायज़ा लिया जाए तो यह दो प्रकार के विषयों से बहस करती हैं। ‘अदबुल-क़ाज़ी’ से सम्बन्धित बहसों की दो क़िस्में हैं। एक प्रकार की बहसें वे हैं जिनका सम्बन्ध शरीअत के मौलिक आदेशों और निर्देशों से है। शरीअत यानी पवित्र क़ुरआन और सुन्नत ने जो कुछ बताया, उसकी रौशनी में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जो कुछ समझा और समझाया, इससे लाभान्वित होकर, उस सबसे मार्गदर्शन लेकर जो सामग्री संकलित की गई वह एक विभाग है। दूसरा विभाग वह है जो प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासनिक सुविधाओं की ख़ातिर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने, क़ाज़ी लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने और अन्य प्रबन्धकों ने अपनी-अपनी बुद्धि और अनुभव की रौशनी में ईजाद किया। ये दोनों अलग-अलग विभाग हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।
सबसे पहला विभाग जिसमें अस्ल और मौलिक हैसियत पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेश रखते हैं। इसका आधार normative है। यानी मुसलमानों के लिए और आगे आनेवालों के लिए क़ानून का स्रोत और मार्गदर्शन और निर्देशन का मूलस्रोत है। यह हिस्सा या विभाग ‘अदबुल-क़ाज़ी’ के बारे में शरीअत के आदेशों की समझ का एक ज़रिया है। शरीअत पर कार्यान्वयन उनकी वजह से आसान होता है। यह विभाग छः चर्चाओं पर सम्मिलित है।
1. सबसे पहली बहस यह है कि स्वयं न्याय व्यवस्था क्या है। क़ाज़ी (न्यायधीश) कौन हो, उसके गुण और विशेषताएँ क्या हों, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, यह ज़िम्मेदारियाँ कौन निर्धारित करेगा, क़ाज़ी अगर अपने कर्तव्य सही तरह से न निभाए तो निगरानी कौन करेगा, निगरानी के करनेवाले के अधिकार और सीमाएँ क्या होंगी। यह अपनी जगह एक बहुत बड़ा मैदान है जिसपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने हज़ारों पृष्ठ लिखे हैं और उनमें से हर चीज़ सीधे क़ुरआनी आयतों या हदीस पर आधारित या इससे उद्धृत है।
2. दूसरा बड़ा विभाग है ‘दावा और उसके अहकाम’। जब आप अदालत में जाएँगे और मुक़द्दमा शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है आपका वह मुक़द्दमा किसी दावे के आधार पर होगा। एक पक्ष दावा दायर करेगा तो फिर मुक़द्दमा चलेगा। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क्या हर मामले के लिए किसी-न-किसी पक्ष की तरफ़ से दावा दायर किया जाना ज़रूरी है। यह बात आज से बारह सौ वर्ष पहले इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने लिखी थी जिसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि हर मामले में यह ज़रूरी नहीं कि इसका किसी निर्धारित व्यक्ति की ओर से दावा दायर किया जाए। कुछ मुक़द्दमों में दावा ज़रूरी है। कुछ के लिए दावा ज़रूरी नहीं है। अदालत ख़ुद से कार्रवाई करके बिना किसी दावे के भी पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति को उसका हक़ दिला सकती है। पिछले तीस-चालीस वर्षों में पश्चिमी दुनिया में यह तसव्वुर आया है कि हर मामले का दावा ज़रूरी नहीं है। आपने एक शब्दावली सुनी होगी जो अदालतों में प्रयुक्त होती है Public Welfare Litigation या Public Litigation Cases या Public Interest Litigation. इस तरह के मुक़द्दमों में कोई निर्धारित मुद्दई (वादी) नहीं होता, लेकिन अदालत ख़ुद से कार्रवाई करते हुए suo moto action ले सकती है। ख़ुद से नोटिस लेने का तसव्वुर पश्चिम में अभी ताज़ा है और सौ पचास वर्षों से ज़्यादा नहीं है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह धारणा पहली सदी में दे दी थी। हदीसों से इसका समर्थन होता है। इस धारणा का आधार भी कुछ हदीसों पर है। कुछ हदीसों से इस बात का इशारा मिलता है कि कुछ मुक़द्दमे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए किसी निर्धारित दावे की आवश्यकता न हो। जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जो संख्या में तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें इंसाफ़ की प्राप्ति के लिए दावा दायर करना ज़रूरी है। ऐसे मुक़द्दमों में प्रभावित एवं प्रताड़ित पक्ष को पहले अदालत में दावा करना चाहिए। इन दोनों मुक़द्दमों में अन्तर क्या है। दोनों के आदेश क्या हैं। वादी (मुद्दई) की शर्तें क्या हैं, प्रतिवादी (मुद्दआ-अलैह) की शर्तें क्या हैं, वादी दावा कैसे लिखे, दावे का जवाब कैसे लिखा जाए। यह एक बहुत बड़ा मैदान है जिसपर अलग से किताबें लिखी गई हैं। अरब दुनिया के एक समकालीन फ़क़ीह ने दो भागों में एक विद्वतापूर्ण किताब लिखी है, ‘नज़रियतुद-दावा बैनश-शरीआ वल-क़ानून’। इसमें उन्होंने दावे की धारणा की शरीअत और पश्चिमी क़ानूनों में तुलना की है।
3. तीसरा बड़ा विभाग ‘क़ानूने-शहादत’ यानी Law of Evidence का है कि किन गवाहियों या किन चीज़ों के आधार पर मुद्दई का दावा स्वीकार या रद्द किया जाएगा। सुबूत के ये माध्यम विस्तार से इस विभाग में चर्चा में आते हैं जिनका आम शीर्षक ‘बय्यिनात’ है। सुबूत के इन माध्यमों में मौखिक गवाही भी शामिल है, इसमें ‘क़रीना-ए-क़ातेआ’ यानी circumstantial evidence (परिस्थितिजन्य साक्ष्य) भी शामिल है। इस लिस्ट में दस्तावेज़ात और हलफ़िया बयानात भी शामिल हैं। इसमें लगभग पंद्रह चीज़ें शामिल हैं जिनमें से कुछ के बारे में मतैक्य है कि वे अदालत में स्वीकार्य हैं, और कुछ के बारे में मतैक्य नहीं है। इन पंद्रह में से लगभग आठ सुबूत के माध्यम प्रत्यक्ष रूप से पवित्र क़ुरआन में बयान हुए हैं। कुछ हदीसों में बयान हुए हैं और कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने तर्कों से मालूम किए हैं। यही आख़िरी माध्यम हैं जिनके बारे में फ़ुक़हा के दरमियान मतभेद है। सुबूत के जो माध्यम पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से साबित हैं उनमें तो कोई मौलिक मतभेद नहीं। यह अपने-आपमें एक अलग विषय है कि इस्लाम का ‘क़ानूने-शहादत’ क्या है। इसपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) शुरू से किताबें लिखते चले आ रहे हैं। फिर उनमें से हर एक विषय पर अलग-अलग किताबें हैं। मौखिक गवाही पर अलग हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (circumstantial evidence) पर अलग हैं, दस्तावेज़ात पर अलग हैं। पवित्र क़ुरआन में सूरा-2 बक़रा और हदीसों में दस्तावेज़ात के बारे में मार्गदर्शन हैं।
4. ‘अदबुल-क़ाज़ी’ का चौथा बड़ा विभाग वह है जिसको ‘सिफ़तुल-हकम’ कहते हैं। इस विभाग में जिस मौलिक मामले से बहस की जाती है वह यह है कि जब अदालत मुक़द्दमा सुनने लगे तो इसकी कार्य-प्रणाली क्या हो। पहले मुद्दई (वादी) दावा बयान करे या मुद्दआ अलैह (प्रतिवादी) बयान करे। गवाहियाँ किसकी पहले सुनी जाएँ और किस की बाद में। गवाहों के बारे में पड़ताल की जाए तो कैसे की जाए, अदालत कहाँ लगाई जाई, अदालत जब लगाई जाए तो जज कैसे बैठे। यह शुरू से आख़िर तक जो पूरा अमल है, उनमें मौलिक मार्गदर्शन पवित्र क़ुरआन और हदीसों में मौजूद हैं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अपने रवैये से, ख़ुलफ़ाए-राशिदीन ने अपने सदाचरण से उनकी और अधिक विस्तृत जानकारी दुनिया के सामने रख दी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने दुनिया को दिखा दिया कि पूर्ण और वास्तविक न्याय एवं इंसाफ़ के लिए अल्लाह के क़ानून के एक-एक शब्द और एक-एक अंग का पालन कैसे किया जाए। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में हज़रत उबई-बिन-कअब (रज़ियल्लाहु अन्हु) मदीने के क़ाज़ी थे। उबई-बिन-कअब वह व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया था कि “मेरे सहाबा में सबसे बेहतर क़ुरआन पढ़नेवाले उबई-बिन-कअब हैं। उबई-बिन-कअब (रज़ियल्लाहु अन्हु) की अदालत में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चाचा हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) एक शिकायत लेकर पेश हुए। दोनों पक्ष क़ाज़ी साहब के सामने पेश होने के इरादे से गए। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अदालत में पहुँचकर सलाम किया। क़ाज़ी ने जवाब दिया कि वअलैकुम अस्सलाम या अमीरुल-मोमिनीन। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसी समय आपत्ति की कि यह नियम के ख़िलाफ़ है। मैं एक नागरिक के तौर पर एक शिकायती बनकर आया हूँ और बतौर अमीरुल-मोमिनीन के नहीं आया। आपने मुझे ज़्यादा इज़्ज़त दे दी और विरोधी पक्ष को इतनी इज़्ज़त नहीं दी। यह समानता के ख़िलाफ़ है। क़ाज़ी ने क्षमा चाही और वादा किया कि वह आगे से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे।
हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कूफ़ा में बतौर ख़लीफ़ा रहते थे। उनके अधीन क़ाज़ी ने, जो सहाबी नहीं, ताबिई थे, उनका एक मुक़द्दमा सुना। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मुक़द्दमा दायर किया था। उनके सच्चे होने में कौन शक कर सकता है। अगर मैं क़सम खाकर कहूँ कि इस धरती पर उस समय उनसे ज़्यादा बेहतर और उनसे ज़्यादा सच्चा इंसान मौजूद नहीं था तो मेरी क़सम ग़लत नहीं होगी इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने अधीन क़ाज़ी की अदालत में दावा किया कि यह ज़िरह मेरी है जो इस यहूदी ने चुराई है। अदालत ने सुबूत माँगा। अमीरुल-मोमिनीन ने फ़रमाया कि एक गवाह तो मेरे बेटे हसन-बिन-अली हैं और दूसरे गवाह मेरे ग़ुलाम क़मर हैं। फ़ैसला क्या हुआ। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) का दावा रद्द कर दिया गया क्योंकि बाप के पक्ष में बेटे की गवाही स्वीकार्य नहीं और मालिक के पक्ष में नौकर या ग़ुलाम की गवाही स्वीकार्य नहीं। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कोई आपत्ति नहीं की। कोई नाराज़ न हुए। यह नहीं कहा कि मैं तो ख़लीफ़ा-ए-राशिद हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने जीवन में मेरे जन्नती होने की गवाही दे गए हैं। मेरे सच्चे होने के लाखों मुसलमान गवाह हैं। दूसरी तरफ़ एक यहूदी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि सच्चा है या झूठा। उन्होंने इस तरह कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप वापस चले गए।
यह ‘सिफ़तुल-हकम’ है। इन उदाहरणों और गवाहियों से इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त दरयाफ़्त किए हैं और बहुत विस्तृत आदेश संकलित किए हैं। उदाहरण के रूप में इन आदेशों में लिखा गया है कि जब क़ाज़ी बैठे तो उसकी बैठक ऐसी होनी चाहिए कि वह दोनों पक्षों से समान दूरी पर हो, यह न हो कि एक पक्ष क़ाज़ी के ज़्यादा क़रीब है और दूसरा कम क़रीब। एक अच्छी जगह पर बैठा है और दूसरा बुरी जगह पर बैठा है। यहाँ तक लिखा है कि जब क़ाज़ी देखे तो दोनों की तरफ़ बराबर देखे। यह नहीं कि एक पक्ष की तरफ़ तो पूरा ध्यान है और दूसरे की तरफ़ कम ध्यान है। दूसरा पक्ष यह महसूस न करे कि मुझे महत्व नहीं दिया गया। दोनों अदालत के ध्यान, अदालत के समय और यहाँ तक कि क़ाज़ी की नज़रों से भी समान रूप से लाभान्वित हों, यह भी उसमें लिखा हुआ है। इन बहसों को ‘सिफ़तुल-हकम’ कहा जाता है।
5. पाँचवाँ विभाग ‘इबरा’ कहलाता है। ‘इबरा’ एक बहुत बड़ा विभाग है। इसपर अलग से किताबें हैं और इसकी बहुत सारी क़िस्में हैं। इबरा, इस्क़ात, मक़ासा, यह लंबी बहस है मैं इसके विवरण में इस समय नहीं जाता, लेकिन ‘उसूले-इबरा’ के तहत किसी पक्ष को यह अधिकार है कि वह अकारण मुक़द्दमेबाज़ी से बचने के लिए अगर कोई मामला करे कि मैंने अपना हक़ ख़त्म कर लिया या समझौता करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसके आदेश ‘इबरा’ के अध्यायों में मौजूद हैं।
इस्लाम में अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ
6. छटा हिस्सा है अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ। अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ वे हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से अदालती ज़िम्मेदारियाँ तो अंजाम नहीं देतीं, लेकिन अदालती काम में सहायक बन सकती हैं, उदाहरण के रूप में मुफ़्ती। मुफ़्ती का काम यह है कि वह क़ानून की व्याख्या कर दे। शरीअत के बारे में मार्गदर्शन कर दे। आपका कोई मामला अटका हुआ है, आपका कोई अधिकार है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं कि क्या है, विरासत में आपका हिस्सा कितना है, वसीयत में कितना है, कोई और क्रय-विक्रय का मामला है तो आपका कोई हक़ बनता है कि नहीं बनता। आप जाकर मुफ़्ती से क़ानूनी मसला (क़ानूनी आदेश) मालूम कर लें। आपको क़ानूनी मश्वरा बिना किसी ख़र्चा के मिल जाएगा। यह एक अर्द्ध न्यायिक सेवा या (Semi-judicial service) है।
फिर इस्लामी व्यवस्था में ‘हिस्बा’ की एक संस्था है। ‘हिस्बा’ की संस्था से मुराद एक ऐसी अर्द्ध न्यायिक संस्था है जो आम विवादों और मुक़द्दमों की सुनवाई के बजाय समाज के ख़िलाफ़ किए जानेवाले अपराधों को सुनने का ज़िम्मेदार हो। ‘हिस्बा’ की संस्था दो पक्षों के दरमियान मुक़द्दमों की नहीं, बल्कि कुल मिलाकर पूरे समाज के ख़िलाफ़ अपराधों की शिकायतों की सुनवाई करता है। वे शिकायतें जिनका सम्बन्ध इस्लाम के नैतिक आचरण से हो, आम नैतिक आचरण या पब्लिक नैतिक आचरण के उल्लंघन की शिकायतें ‘मुहतसिब’ (लोकपाल) की अदालत में जाएँगी और वह इस बारे में कार्रवाई करेगा। एक व्यक्ति घटिया प्रकार का गेहूँ बेच रहा है। अब न आपने वह गेहूँ ख़रीदा है और न ही आपका उस लेन-देन से सीधा कोई सम्बन्ध है इसलिए आम क़ानून की दृष्टि से आप इस मामले में पक्ष नहीं बन सकते। इसलिए अदालत कहेगी कि आपको क्या शिकायत है? लेकिन ‘मुहतसिब’ इसपर आपत्ति कर सकता है और मुक़द्दमा दर्ज कर सकता है क्योंकि वह पब्लिक लेटिगेशन का ज़िम्मेदार है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं इस संस्था को क़ायम किया और इसके काम का संरक्षण किया। वे समय-समय पर बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते थे। विभिन्न इलाक़ों का दौरा करते और जहाँ कोई ऐसी शिकायत होती उसको दूर करते। एक-बार वे बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, गेहूँ का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने क़ीमत पूछी। गेहूँ के ढेर में हाथ डालकर थोड़ा-सा गेहूँ बाहर निकाला तो वह गीला था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि यह क्या है? दुकानदार ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल! ये लोग गीला गेहूँ ख़रीदते नहीं और यह बारिश में गीला हो गया था, इसलिए मैंने ख़ुश्क गेहूँ ऊपर कर दिया है और गीला नीचे कर दिया है, ताकि लोग ख़रीदने में संकोच न करें। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “जो लोगों को धोखा दे वह हम में से नहीं है।” यानी तुम गीला गेहूँ ऊपर रखूँ, जिसका जी चाहेगा वह गीला ख़रीदेगा और जिसका दिल नहीं चाहेगा वह नहीं ख़रीदेगा। तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है कि तुम लोगों को धोखा देने के लिए ख़ुश्क गेहूँ ऊपर और गीला नीचे रख दो।
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इस संस्था को और विस्तार दिया तथा संगठित किया और विस्तृत पैमाने पर स्वयं भी इसके लिए काम किया। उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जगह-जगह ‘मुहतसिब’ नियुक्त किए। एक उल्लेख में आता है, जिससे कुछ लोगों ने मतभेद भी किया है कि शिफ़ा-बिंते-अबदुल्लाह अनसारिया एक महिला थीं। उनको एक बाज़ार का, जहाँ महिलाएँ बहुत आती-जाती थीं, मुहतसिब नियुक्त किया गया था। उनकी ज़िम्मेदारी यह थी कि वह उस बाज़ार की निगरानी करें कि वहाँ के काम शरीअत के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं।
‘हिस्बा’ की संस्था समय गुज़रने के साथ-साथ विकास और विस्तार की मंज़िलें तय करती रही। दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमानों की सरकारें क़ायम हुईं, वहाँ ‘हिस्बा’ के संस्था भी क़ायम हुई। एक ओर मुसलमान शासक क़ाज़ी और दूसरे विद्वान ‘हिस्बा’ के प्रबन्धन सम्बन्धी पहलुओं पर ध्यान दे रहे थे और इस संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबन्धन सम्बन्धी नए-नए उपाय अमल में ला रहे थे। दूसरी तरफ़ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) नित नए अनुभवों और प्रबन्धों के फ़िक़ही आदेश संकलित कर रहे थे। इस तरह स्वयं ‘हिस्बा’ एक महत्वपूर्ण फ़िक़ही विषय बन गया जिसपर बहुत-सी किताबें लिखी गईं। आज भी इस्लामी पुस्तकालयों में ‘हिस्बा’ के विषय पर दर्जनों किताबें अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में मौजूद हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इस विषय पर प्राचीन किताबों में एक महत्वपूर्ण किताब साम्राज्य काल के प्रसिद्ध फ़क़ीह और क़ाज़ी अल्लामा ज़ियाउद्दीन सुनामी की ‘निसाबुल-इहतिसाब है जिसका उल्लेख ‘हिस्बा’ पर लिखनेवाले बहुत-से लोगों ने किया है। यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी। इस तरह की संस्थाएँ जिनकी संख्या छः है उनको अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ कहा जाता है। ये वे संस्थाएँ हैं जो अर्द्ध न्यायिक कर्तव्य निभाती हैं। उनमें ‘हिस्बा’ के अलावा अन्य उल्लेखनीय संस्थाएँ ये हैं—
1. दीवाने-मज़ालिम
2. दीवाने-जराइम
3. इफ़्ता
4. तहकीम
5. वकालत बिल-ख़ुसूमत
दीवाने-मज़ालिम हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ायम किया था। इसका उद्देश्य आम और कमज़ोर नागरिकों को प्रभावशाली व्यक्तियों और बेलगाम अधिकारियों की ज़्यादतियों और बद इंतिज़ामियों से सुरक्षित रखना था। यह लगभग इसी तरह की चीज़ थी जिसको आज ombudsman कहा जाता है। यह संस्था आला सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायतें सुनती और आम आदमी को उसका समाधान उपलब्ध करती थी। यह संस्था हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ायम की थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) समय-समय पर ‘मुहतिसब’ व्यक्तियों या दीवाने-मज़ालिम के उच्चाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया करते थे। वे मार्गदर्शन आज विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित रूप में मौजूद और उपलब्ध हैं। फिर कुछ अदालतें ऐसी क़ायम हुई थीं जिनका सम्बन्ध फ़ौजदारी मुक़द्दमों से था। उनके आदेश अलग हैं जिसके बारे में किताबें उपलब्ध हैं।
कुछ अदालतें वे थीं जो अन्य प्रकार के मामलों उदाहरणार्थ माली मामलों को देखती थीं। यह ‘अदबुल-क़ाज़ी’ का वह हिस्सा है जिसके आदेश सीधे पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से उद्धृत हैं।
‘अदबुल-क़ाज़ी’ का दूसरा हिस्सा वह था जो प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अस्तित्व में आया और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने अनुभव और बुद्धि के प्रकाश में जनसाधारण की सुविधा की ख़ातिर उसके आदेश संकलित किए। उनमें से एक कला ‘इल्मुश-शुरूत’ कहलाती है। ‘शर्त’ का बहुवचन ‘शुरूत’ (शर्तें) है। ‘इल्मुश-शुरूत’ के शाब्दिक अर्थ हैं The Science of Condtions. लेकिन इससे मुराद वह ज्ञान था जिसको आजकल दस्तावेज़ लेखन कहते हैं। अगर आप में किसी ने एल.एल.बी किया हो या लॉ कॉलेज में पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि एल.एल.बी. के आख़िरी वर्ष में एक पर्चा पढ़ाया जाता है, जिसका शीर्षक ही दस्तावेज़ात या Conveyancing and pleadings है। इसमें यह बताया जाता है कि वकील दस्तावेज़ात कैसे लिखे। मुक़द्दमे की अन्य दस्तावेज़ात, दावा और दावे का जवाब वग़ैरा कैसे तैयार करे। यह एक बड़ी विकसित और लोकप्रिय कला थी जिसपर बहुत-से फ़ुक़हा ने काम किया और किताबें लिखीं। इस कला को ‘इल्मुश-शुरूत’ कहा जाता है।
इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इस कला को ईजाद किया। उनसे पहले अलग से दस्तावेज़ लेखन की यह कला मौजूद नहीं थी। उन्होंने इसपर किताबें लिखीं। इमाम अबू-ज़ैद अश-शुरूती एक फ़क़ीह थे। उन्होंने ‘शुरूत’ (शर्तों) में इतनी दक्षता पैदा की कि उनका नाम ही शुरूती पड़ गया। उन्होंने तीन किताबें लिखीं, ‘किताबुश-शुरूत अस-सग़ीर’, ‘किताबश-शुरूत अल-कबीर’ और ‘किताबुश-शुरूत अल-वसीत’। इनमें से एक ‘किताबुश-शुरूत अस-सग़ीर’ आज हमारे पास मौजूद है। जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी उपलब्ध है। इस किताब से यह पता चलता है कि उनकी राय में दस्तावेज़ लिखने का तरीक़ा क्या था।
ये कला जिस बुज़ुर्ग की ईजाद है वह इमाम शाफ़िई (रह॰) हैं। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने सबसे पहले दस्तावेज़ात की कला को अपनी दिलचस्पी का विषय बनाया। स्वयं उन्होंने कई दस्तावेज़ात तैयार कीं। इमाम शाफ़िई (रह॰) की तैयार की हुईं पाँडुलिपियाँ आज उनकी किताब ‘किताबुल-उम्म’ में मौजूद हैं। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने इन दस्तावेज़ात के नमूने देकर यह दिखाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन हो तो इस तरह की दस्तावेज़ होगी। हल्का लेन-देन होगा तो इस तरह की दस्तावेज़ होगी, अमुक मामला हो तो इस तरह की दस्तावेज़ होगी। यह कला सबसे पहले इमाम शाफ़िई (रह॰) ने संकलित की। उनके बाद शेष फ़ुक़हा ने भी इसपर काम किया। लेकिन जिस उल्लेखनीय फ़क़ीह ने विधिवत रूप से किताब लिखी और वह हम तक भी पहुँची, वह इमाम अबू-ज़ैद शुरूती हैं जिनकी एक किताब आज भी उपलब्ध है।
दूसरी कला कहलाती था ‘इल्मुल-महाज़िर’। ‘महज़र’ का बहुवचन ‘महाज़िर’ है और इसका अर्थ हैं minutes यानी कार्रवाई। यानी इस कला में यह बताया जाता था कि मुक़द्दमे की कार्रवाई कैसे लिखी जाए। जज स्वयं लिखे, अदालती अधिकारी लिखें, कोई पक्ष लिखे, उसका तरीक़ा क्या होगा, उसका फ़ॉर्मेट क्या होगा। जिन इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘इल्मुल-महाज़िर’ पर लिखा उन्होंने उसके नमूने और फ़ॉर्मेट भी तैयार करके दिए। इस तरह के फ़ॉर्मेट आज भी बने हुए मौजूद हैं। लेकिन ‘इल्मुल-महाज़िर’ की ये प्राचीन किताबें आज बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं हैं, क्योंकि आज फ़ॉर्मेटिंग का तरीक़ा विभिन्न है और दस्तावेज़ात और तरह से लिखी जाती हैं। अदालती कार्रवाई लिखने की कार्य-प्रणाली शायद आजकल ज़्यादा विकसित है। आज कंप्यूटर का ज़माना है और हर चीज़ उसमें मौजूद है। लेकिन इन किताबों का यह महत्व ज़रूर है कि उनसे पता चलता है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इन समस्याओं पर बारह तेरह सौ वर्ष पहले सोचा, जिनसे पश्चिमी जगत् अब सौ दो सौ वर्ष पहले परिचित हुई है।
फिर जब मुक़द्दमा पूरा हो जाए और फ़ैसला सुना दिया जाए तो मुक़द्दमों का रिकार्ड कैसे रखा जाए, इस कला को ‘इल्मे-सिजल्लात’ कहते थे। ‘सिजल’ का अर्थ रजिस्टर है। ‘सिजल्लात’ से मुराद वह कला थी जिसमें दस्तावेज़ात को तैयार करने और सुरक्षित रखने के तरीक़े दर्ज हैं। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसपर भी किताबें लिखी हैं। अगर आपकी पहुँच किसी ऐसे पुस्तकालय तक हो जहाँ फ़तावा आलमगीरी का उर्दू अनुवाद मौजूद हो, जो दस भागोंवाला है, इसमें नौवाँ भाग उठाकर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें यानी ‘महाज़िर’, ‘सिजल्लात’ और ‘शुरूत’ (शर्तें) सब मौजूद हैं। और यह बताया गया है कि दस्तावेज़ात कैसे रखी जाएँ। इसमें दस्तावेज़ रखने का तरीक़ा वह था जिसको आजकल स्क्रॉल कहते हैं, क्योंकि क़लमी किताबें होती थीं। क़लमी किताबें रखना और लिखना मुश्किल होता था, तो किताबें स्क्रॉल के रूप में रखी जाती थी। लंबी दस्तावेज़ होती थी उसको लपेटकर रखते थे। इस तरह के प्राचीन स्क्रॉल मदीना मुनव्वरा में सुरक्षित हैं। उनमें चौथी पाँचवीं सदी तक के कुछ फ़ैसले मौजूद हैं। इस तरह के सक्रॉल क़ाहिरा में भी मौजूद हैं जिनमें पाँचवीं-छठी सदी हिजरी के फ़ैसले मौजूद हैं। हमारे बहावलपुर में भी इस तरह का एक म्यूज़ियम है जिसमें इसी तरह के स्क्रॉल मौजूद हैं और जिनमें पूर्व अदालतों के मुक़द्दमों की कार्रवाइयाँ लिखी हुई हैं। प्राचीनतम, आज से तीन साढ़े तीन सौ वर्ष पहले के मुक़द्दमे मौजूद हैं, जो मैंने देखे हैं।
यह ‘अदबुल-क़ाज़ी’ का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय है जो फ़िक़्हे-इस्लामी का एक महत्वपूर्ण विभाग है और यह उसके ज़ेली विभाग हैं। इन ज़ेली विभागों में से हर विभाग पर अलग-अलग किताबें हैं जिनसे आपको अनुमान हो जाएगा कि यह कला कितनी फैली हुई है। फ़तवा और आदाबे-फ़तवा (फ़तवा देने के नियमों) पर अलग से किताबें लिखी गई हैं कि मुफ़्ती कौन हो, फ़तवे के अदाब क्या होंगे और वह कैसे फ़तवा देगा। तुलनात्मक अध्ययन क़ानून का ज्ञान आजकल क़ानून का एक विभाग है जिसको comperative law कहते हैं, यानी क़ानून का तुलनात्मक अध्ययन। यह कला भी मुसलमान फ़ुक़हा की ईजाद है। क़ानूनी राय, फ़िक़ही इख़तिलाफ़ और उसके कारण पर अपनी-अपनी किताबों में तो लगभग हर बड़े फ़क़ीह ने चर्चा की और दूसरी बहसों के सन्दर्भ में फ़ुक़हा के मतभेदों पर भी बहस की। इमाम शाफ़िई (रह॰), इमाम मालिक (रह॰), इमाम मुहम्मद और इमाम अबू-यूसुफ़ ने अपनी-अपनी किताबों में जहाँ महत्वपूर्ण फ़िक़ही मामलों पर अपनी और दूसरों की रायों और इज्तिहादात को क़लम-बंद किया वहाँ फ़ुक़हा के मतभेदों और इसके कारणों पर भी चर्चा की, लेकिन जिस फ़क़ीह ने ख़ास इस विषय पर अलग से किताब लिखी कि विभिन्न क़ानूनी या फ़िक़ही मामलों में विभिन्न क़ानूनविदों की राय क्या है, वे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं अल्लामा इब्ने-जरीर तबरी। इब्ने-जरीर तबरी इतिहासकार भी हैं, क़ुरआन के टीकाकार भी हैं और बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं। उनकी किताब ‘इख़्तिलाफ़ुल-फ़ुक़हा’ इस विषय पर प्राचीनतम उपलब्ध किताब है। इस किताब का विषय ही यह है कि फ़ुक़हा की जो विभिन्न रायें हैं उनके कारण क्या हैं और उन कारणों के परिणामस्वरूप जो विभिन्न रायें पैदा हुईं वे क्यों पैदा हुईं, इन रायों को एक-दूसरे के क़रीब कैसे लाया जा सकता है, इन रायों पर अमल करने के परिणामस्वरूप समस्याएँ और मुश्किलें क्या पैदा हो सकती हैं, यह विषय इमाम इब्ने-जरीर तबरी की किताब ‘इख़्तिलाफ़ुल-फ़ुक़हा’ का है। कई और महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिनपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बहुत अधिक लिखा है। उनमें से अनेक विषयों की हैसियत फ़िक़्हे-इस्लामी के महत्वपूर्ण विभागों और उप-विषयों की है। लेकिन समय की तंगी के कारण वे रह गए। इंशा अल्लाह आगे चलकर जब इज्तिहाद पर बात होगी या शरई आदेशों की तत्वदर्शिता पर चर्चा होगी तो उनमें कुछ एक का मैं ज़िक्र करूँगा।
फ़ुक़हा के ज्ञानपरक नियम
एक आख़िरी चीज़ जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की बड़ी अजीबोग़रीब देन है, उसको ‘क़वाइदे-फ़िक़हीया’ कहते हैं। ‘क़वाइदे-फ़िक़हीया’ से मुराद वह मौलिक नियम और सिद्धान्त हैं जिनसे फ़िक़्हे-इस्लामी के आंशिक आदेशों को समझने में सहायता मिलती है। अगर ‘क़वाइदे-फ़िक़हीया’ सामने हों तो बहुत-से आदेशों को समझने में सुविधा हो जाती है। उदाहरण के रूप में एक फ़िक़ही नियम है ‘असल यह है कि जो चीज़ पहले मौजूद थी उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह अभी तक मौजूद है जब तक कि उसका न होना साबित न हो जाए’। यह उसूल प्रत्यक्ष रूप से कुछ हदीसों से उद्धृत है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बीमार रहता हूँ। मेरा मेदा (यकृत) ख़राब है और गैस का रोगी हूँ। मुझे कभी-कभी यह सन्देह हो जाता है कि वुज़ू टूट गया। घर से वुज़ू करके निकलता हूँ, लेकिन मस्जिद तक पहुँचते-पहुँचते पेट से आवाज़ें आती हैं तो सन्देह हो जाता है कि शायद वुज़ू टूट गया। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि जब तुम वुज़ू करके घर से निकले हो, तो जब तक विश्वास न हो जाए, और विश्वास के सुबूत बताए कि ये-ये सुबूत हैं जिनसे वुज़ू टूटने का विश्वास हो जाता है, अत: जब तक विश्वास न हो जाए उस समय तक वुज़ू क़ायम है। इससे इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह उसूल निकाला कि जो चीज़ पहले मौजूद थी उसको उस समय तक मौजूद समझा जाएगा जब तक किसी पक्की दलील से उसका मिट जाना साबित न हो जाए। जब वे सहाबी घर से निकले तो वुज़ू मौजूद था और जब तक निश्चित तौर पर साबित न हो जाए कि अब वुज़ू नहीं रहा उस समय तक आप यह समझें कि वुज़ू क़ायम है। इससे यह क़ायदा उद्धृत है।
अब अगर आपके ज़ेहन में यह क़ायदा हो, तो आपको मफ़क़ूद (खोए हुए) व्यक्ति के प्रसिद्ध मसले के बारे में फ़ुक़हा किराम विशेषकर इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की राय को समझने में बड़ी सुविधा होगी। एक मसला यह पैदा हुआ कि अगर किसी महिला का पति गुम हो जाए तो वह कब तक उसकी प्रतीक्षा करे? क्या वह मरते दम तक उसकी प्रतीक्षा में बैठी रहे, या क्या करे? कुछ पता नहीं कि मर गया या ज़िन्दा है। यह पुराने-ज़माने के सफ़रों में बहुत होता था कि एक आदमी किसी काम से उदाहरणार्थ चीन गया। अब वहाँ से न उसका कोई पत्र आता है न टेलीफ़ोन है न सम्पर्क का कोई और ज़रिया है। वर्षों पता नहीं चलता था कि वह आदमी ज़िन्दा है कि मुर्दा है। ऐसे मौक़ों पर पत्नी क्या करे। वह उसको मुर्दा क़रार देकर अलग हो जाए, या इद्दत पूरी करके दूसरा निकाह कर ले, आख़िर क्या करे? इस बारे में पवित्र क़ुरआन में कोई स्पष्ट आयत मौजूद नहीं। ‘नस्से-सरीह’ हदीसों में भी नहीं है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में जिहाद अरब द्वीप तक सीमित था। व्यापार भी क़रीब-क़रीब के इलाक़ों तक था और क़ाफ़िले भी बहुत अधिक आया-जाया करते थे। इसलिए यह स्थिति पैदा नहीं होती थी कि किसी व्यक्ति का सालों तक पता ही न चले कि ज़िन्दा है या मर गया है। बाद के ज़माने में जब अफ़्रीक़ा के मरुस्थलों और चीन में गोबी मरुस्थल और मंगोलिया से आगे जिहाद होता था तो लोग छः छः महीने की यात्रा पर जाते थे और वर्षों तक वहाँ इस्लाम के प्रचार-प्रसार, जिहाद या व्यापार में मसरूफ़ रहकर कई-कई वर्ष में लौटते थे। कुछ स्थितियों में आदमी लापता हो जाता था तो दसियों वर्ष ख़बर न होती कि कहाँ गया। इन हालात में यह समस्या बहुत गम्भीर हो गई।
ऐसी स्थिति में विभिन्न फ़ुक़हा ने अपनी-अपनी बुद्धि और समझ से इसपर राय दी। इसपर विस्तार में जाने का मौक़ा नहीं। संक्षेप में बताता हूँ। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने यह राय दी कि जब तक उस व्यक्ति के समय और उम्र के लोग ज़िन्दा हैं उस समय तक उसको ज़िन्दा समझा जाएगा और उसकी पत्नी को न तलाक़ होगी, न वह इद्दत में बैठेगी और न दूसरा निकाह करेगी। अब बज़ाहिर यह बहुत मुश्किल था कि गुमशुदा आदमी के दोस्त अगर अस्सी-नव्वे वर्ष की उम्र तक ज़िन्दा रहें तो आप उसकी पत्नी को भी अस्सी-नव्वे वर्ष की उम्र तक प्रतीक्षा कराएँ। उस उम्र में वह क्या निकाह करेगी। दूसरे निकाह की समस्या तो जवानी में पैदा हो सकती है। अस्सी-नव्वे वर्ष की उम्र में निकाह की क्या आवश्यकता पेश आ सकती है।
लेकिन इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की यह राय जो बज़ाहिर बड़ी अजीब-ग़रीब मालूम होती है वह इसी नियम के आधार पर है कि अगर शरीअत का उसूल यह है कि जो पहले मौजूद है उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह आगे भी मौजूद है। जब तक कि इसका न होना साबित न हो जाए। अब बौद्धिक दृष्टि से यह उनकी राय बड़ी मज़बूत है। लेकिन इससे और बहुत-सी सामाजिक और नैतिक मुश्किलें पैदा हुईं तो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘इस्तेहसान’ से काम लिया, अनुमान से काम नहीं लिया। और इसका दूसरा समाधान प्रस्ताव किया जिसका अब दुनिया में पालन होता है।
यों एक-एक करके फ़िक़्ह के सैंकड़ों नियम तैयार होते गए। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने सहाबा के ज़माने से यह ‘क़वाइदे-फ़िक़हीया’ दरयाफ़्त करने शुरू किए और जैसे-जैसे उलमा और फ़ुक़हा पवित्र क़ुरआन और शरीअत के आदेशों पर ग़ौर करते गए तो इस तरह के नियम निकलते गए। इन नियमों को अलग-अलग किताबों के रूप में संकलित किया जाता रहा। इन नियमों की खोज के दो तरीक़े थे। एक तरीक़ा तो यह था कि शरीअत के आदेशों पर चिन्तन-मनन करके मिलते-जुलते आदेश (यानी इश्बाह और नज़ाइर) की निशानदेही की जाए और फिर इन आदेशों की एक-दूसरे से तुलना करके वे आम सिद्धान्त निकाले जाएँ जो इन मिलते-जुलते इश्बाह एवं नज़ाइर के आदेशों में समान हैं। इस कला यानी इश्बाह और नज़ाइर का उल्लेख सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के एक प्रसिद्ध लेख्य में मिलता है। जैसा कि फ़िक़्हे-इस्लामी के इतिहास के छात्र भली-भाँति परिचित हैं, हज़रत उमर-फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक प्रसिद्ध पत्र हज़रत अबू-मूसा अशअरी को लिखा था।
इल्मे-इश्बाह और नज़ाइर
हज़रत अबू-मूसा अशअरी बस्रा के चीफ़ जस्टिस थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उन्हें अदालती पॉलिसी के बारे में एक ख़त लिखा था। इस ख़त में बहुत-से निर्देश थे जो अत्यन्त क़ीमती सिद्धान्तों पर आधारित हैं। इसमें यह लिखा था कि इश्बाह और नज़ाइर का अध्ययन करो और मिलते-जुलते मामलात को एक-दूसरे पर अनुमान करो। यहाँ से इल्मे-इश्बाह एवं नज़ाइर का भी आरम्भ हुआ। इस ज्ञान का शरीअत के उद्देश्य के इन आदेशों और नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करना है जो बज़ाहिर एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। शरीअत के आदेशों में ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं कि दो मामलात एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। उदाहरणार्थ वुज़ू और तयम्मुम एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। दोनों के आदेशों में कुछ बातें समान हैं, कुछ बातें भिन्न हैं। अब जो समान हैं उनपर ग़ौर करके पता चलाया जाए कि वे क्यों समान हैं। यह एक ग़ौर करने की बात है। या उदाहरणार्थ गवाही और अदालती फ़ैसले, यह दोनों भी मिलती-जुलती चीज़ें हैं। हदीस की रिवायतें और फ़तवा, दोनों मिलती-जुलती चीज़ें हैं। आप एक आलिम के पास जाएँ और पूछें कि क्या इस विषय पर कोई हदीस मौजूद है? वह आपको हदीस सुना दे। तो यह रिवायते-हदीस हुई। फ़तवा यह है कि आप एक आलिम से सवाल करें कि इस मसले का जवाब क्या है। और वह हदीस सुनादे। दोनों बार उन्होंने हदीस सुनाई। एक बार बतौर रिवायत के और दूसरी बार बतौर फ़तवा के हदीस सुनाई। बज़ाहिर दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन दर-हक़ीक़त यह दोनों एक चीज़ नहीं हैं।
इल्मे-फ़ुरुक़ और इल्मे-इश्बाह तथा नज़ाइर
इस तरह की इकट्ठी चीज़ों पर ग़ौर करके जब उनको जमा किया गया तो उन मिलती-जुलती चीज़ों को इश्बाह एवं नज़ाइर कहा गया। इसपर अलग से अनेक किताबें मौजूद हैं। यह एक कला है जो अपनी जगह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और मुश्किल कला है। इन मामलों पर ग़ौर किया तो ग़ौर करने के बाद कहीं तो यह पता चला कि ये दोनों बिलकुल एक जैसी चीज़ें हैं। कहीं पता चला कि बज़ाहिर तो दोनों चीज़ें मिलती-जुलती हैं, लेकिन वास्तव में एक नहीं, अलग-अलग हैं। फिर इसपर ग़ौर किया गया कि जो चीज़ें अलग-अलग साबित होती हैं, वे क्यों अलग हैं, और उनमें क्या अन्तर है। तो इस तरह के मसाइल जमा किए गए और उनको ‘इल्मुल-फ़ुरूक़’ कहा जाने लगा, जो मिलती-जुलती चीज़ों का ज्ञान है वह ‘इश्बाहुन-नज़ाइर’ कहलाया गया।
फ़ुरुक़ पर एक बड़ी मोटी किताब है जिसके बारे में मैं यह समझता हूँ कि शायद मानवता के पूरे इतिहास में इस जैसी कोई और किताब नहीं है। वह अल्लामा उबुल-अब्बास क़राफ़ी की ‘किताबुल-फ़ुरूक़’ है जो चार भागों में है। इसलिए कि शरीअत के अलावा फ़ुरुक़ के ज्ञान का कोई विकल्प किसी क़ौम के पास मौजूद नहीं है। इल्मे-फ़ुरुक़ दुनिया में मुसलमानों के अलावा कहीं और पाया नहीं जाता। इल्मे-फ़ुरुक़ पर मुसलमानों में बेहतरीन किताब अल्लामा क़राफ़ी की है इसलिए यही किताब दुनिया के इतिहास में इस कला पर बेहतरीन किताब क़रार पाएगी। यह अल्लामा क़राफ़ी एक फ़क़ीह होने के साथ-साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इन्ही के उल्लेख पर बात समाप्त करता हूँ। उन्होंने घड़ी भी ईजाद की थी, जिसका विवरण किताबों में मिलता हैं। वैज्ञानिक भी थे और फ़क़ीह भी थे। इतने बड़े फ़क़ीह थे कि ‘किताबुल-फ़ुरूक़’ के लेखक हैं जिससे बेहतर किताब ‘फ़ुरुक़’ के बारे में आज तक नहीं लिखी गई। उन्होंने 560 फ़ुरुक़ जमा किए हैं। 560 समस्याएँ जमा की हैं जो बज़ाहिर एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। यह असल में 560 समस्याएँ या उसूल नहीं, बल्कि 1120 उसूल हैं। इसलिए कि हर ‘फ़र्क़’ के अन्तर्गत दो-दो मिलते-जुलते सिद्धान्त बयान किए गए हैं। ये सब वे चीज़ें हैं जो बज़ाहिर तो एक-दूसरे से मिलती-जुलती मालूम होती थीं, लेकिन वास्तव में वे मिलती-जुलती चीज़ें नहीं हैं। उनमें कई दृष्टि से मौलिक अन्तर है। तो 560 शीर्षकों के अन्तर्गत उन्होंने वे चीज़ें बताई हैं जो हर जगह दो हैं और एक जैसी मालूम होती हैं लेकिन एक जैसी नहीं हैं। इश्बाह और नज़ाइर और इल्मे-फ़ुरूक़ दो ऐसे ज्ञान हैं जिनका कोई उदाहरण दुनिया में इस समय तक तो मौजूद नहीं है आगे चलकर अगर सामने आ जाए तो हम नहीं कह सकते।
ये महत्वपूर्ण फ़िक़ही ज्ञान-विज्ञान हैं। उनमें से अधिकतर अध्याय और अंग हैं जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने पहली और दूसरी सदी हिजरी में संकलित किए थे और दुनिया को इन तक आने में कहीं हज़ार, कहीं बारह सौ और कहीं इससे ज़्यादा वर्ष लगे।
यह एक अति संक्षिप्त और सरसरी परिचय था महत्वपूर्ण फ़िक़ही उलूम का। महत्वहीन आंशिक सिद्धान्त मैंने छोड़ दिए। महत्वहीन तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा आंशिक या विस्तृत थे वे मैंने छोड़ दिए हैं। जो ज्ञान-विज्ञान और विभाग मौलिक प्रकार के थे वे मैंने बयान कर दिए हैं। इससे आपको अनुमान हो गया होगा कि यह कितना असाधारण बौद्धिक एवं वैचारिक कारनामा है जो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के हाथों अंजाम पाया। इसी लिए मैंने कहा था कि फ़िक़्हे-इस्लामी इस्लामी ज्ञान-विज्ञान का भंडार है।
सवालात
सवाल : बहुत-से लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं कि नमाज़ जैसा अमल जिसको नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दिन में पाँच बार करके दिखाया, इसमें यह बात हम तक क्यों न पहुँची कि उनकी नमाज़ उनके जीवन के आख़िर में तमाम परिवर्तनों के बाद किस शक्ल में थी? इस बारे में मतभेद का पाया जाना चिन्ताजनक है?
जवाब : मुझे मौलिक मतभेद तो यह है कि इस बारे में मतभेद का होना कोई चिन्ताजनक बात नहीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों के मजमे के सामने नमाज़ें पढ़ीं और विभिन्न ढंग से पढ़ीं। सर्वोच्च अल्लाह ने यह चाहा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नमाज़ में जिस-जिस तरह से किया और जो-जो किया वह सब सुरक्षित रहे। कोई अदा अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ऐसी न हो जो मुसलमानों में सुरक्षित न रहे और मुसलमानों का कोई एक वर्ग न अपनाए। आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कभी-कभी पूरी पूरी रात नमाज़ पढ़ते थे। यहाँ तक कि पाँव मुबारक में सूजन आ जाया करती थी। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु उन्हा) ने एक-बार बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल! पवित्र क़ुरआन में है कि सर्वोच्च अल्लाह ने आपके तमाम अगले-पिछले गुनाह, अगर कोई थे भी, तो माफ़ कर दिए हैं। आप तो पैग़ंबर हैं और बख़्शे गए हैं। फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि “क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ?” कभी-कभी वे पूरी-पूरी रात नवाफ़िल (ऐच्छिक नमाज़ें) पढ़ा करते थे। कभी-कभी मस्जिदे-नबवी में दिन के समय और ख़ास तौर पर ज़ुह्र के बाद लम्बे नवाफ़िल पढ़ने का कभी-कभी रोज़ का नियम होता था। लम्बे नवाफ़िल में जब आदमी हाथ बाँधकर नमाज़ पढ़ता है, तो कभी-कभी हाथ थक जाता है, और हाथ खोलकर नमाज़ पढ़ने में आराम मिलता था।
आप रमज़ान के आख़िरी तीन दिनों में कभी फ़ैसल मस्जिद में आएँ। जहाँ इन तीन रातों में महफ़िले-शबीना होती है जिसमें दस-दस पारे पढ़े जाते हैं। आपको अनुमान हो जाएगा कि एक ही पारा पढ़ने में हाथ दुख जाता है और जब इमाम रुकअ में जाता है और सब हाथ खोलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी लम्बी नमाज़ों में कभी-कभी हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ा करते थे। अब किसी ने देखा कि नबी (सल्ल॰) अपने हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्होंने बयान किया कि हुज़ूर हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ा करते थे। कभी हाथ ऊपर बाँधा और थकने के बाद नीचे बाँध दिया। नीचे थक गया तो ज़रा ऊपर कर लिया, इससे आराम मिल जाता है। इसलिए इसमें न तो किसी वैध या अवैध का मसला है, न इसमें किसी मकरूह और मुस्तहब का मसला है। उनमें से हर कार्य-नीति सुन्नत है और उनमें से हर रवैया अपनी जगह जायज़ है। फ़ुक़हा ने केवल यह सवाल उठाया कि उनमें श्रेष्ठ अमल कौन सा है। अगर मैं इन कामों को करूँ तो कौन-सा पहले करूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। कुछ ने कहा हाथ बाँधकर पढ़ना श्रेष्ठ है। इसपर सबका मतैक्य है कि यह सब सुन्नत का हिस्सा है। इसलिए इसमें किसी चिन्ता की कोई बात नहीं है और न ही इसमें परेशानी की कोई बात है। मुसलमान चौदह सौ बरस से नमाज़ इसी तरह पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, आप परेशान न हों।
आपका जी चाहे तो सूरा फ़ातिहा में आमीन ऊँची आवाज़ से पढ़िए और जी चाहे तो आहिस्ता पढ़िए। जी चाहे तो रफ़ा-यदैन करें और जी न चाहे तो न करें। सब सूरतें जायज़ हैं। सब सुन्नत हैं और सबके सुन्नते-साबिता होने में कोई शक-सन्देह नहीं। न ये चीज़ें मुसलमानों में बिखराव का कारण हैं, न इनसे मतभेद पैदा होता है। हरम शरीफ़ में जाकर देखें। लाखों व्यक्ति कई-कई तरीक़ों से नमाज़ पढ़ते नज़र आते हैं। कोई ज़ोर से आमीन कहता है। कोई आहिस्ता से कहता है। सब एक-दूसरे से गले मिलते हैं और कोई लड़ता नहीं। यह तो हमारे यहाँ इन मामलों को इख़्तिलाफ़ का ज़रिया बना दिया गया है। सच्चाई तो यह है कि हमारे यहाँ लड़ने के कारण और हैं। उनका आमीन ज़ोर से या आहिस्ता कहने से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही इसका रफ़ा-यदैन से कोई सम्बन्ध है। नमाज़ के अन्दर रफ़ा-यदैन करने से कोई झगड़ा नहीं होता। हाँ नमाज़ से बाहर रफ़ा-यदैन (हाथ उठाने) करने से झगड़ा होता है। जब जाहिल और पक्षपाती लोग एक-दूसरे पर रफ़ा-यदैन करते (हाथ उठाते) हैं। इससे हर मुसलमान को बचना चाहिए।
सवाल : इस्लामी फ़िक़्ह पर उर्दू में किसी अच्छी किताब की निशानदेही करें।
जवाब : उर्दू में दो तीन किताबें अच्छी हैं। एक अच्छी किताब जो मुझे बहुत पसंद है वह भारत
के मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी ने ‘आसान फ़िक़्ह’ के नाम से लिखी है। दो मोटे भागों में है। पाकिस्तान में कई बार छपी है। वह अच्छी किताब है। दूसरी किताब भी भारत ही के मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी की है। यह इस्लामी फ़िक़्ह के नाम दो मोटे भागों में है और कई बार छपी है। एक और कुछ संक्षिप्त किताब है आसान फ़िक़्ह, मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ इस्लाही की, यह बुज़ुर्ग भी भारत के रहनेवाले हैं। अस्लन पाकिस्तानी हैं, हज़ारा से उनका सम्बन्ध है। लेकिन वे भारत-विभाजन के समय भारत में आबाद थे और वहीं रह गए। उनकी किताब ‘आसान फ़िक़्ह’ भी अच्छी किताब है।
इस समय मेरे ज़ेहन में ये तीन किताबें आ रही हैं और भी बहुत-सी किताबें हैं। सरसरी और आरम्भिक अध्ययन के लिए ये किताबें बहुत काफ़ी हैं।
सवाल : पति के गुम होने पर आपने मसला बयान किया जो स्पष्ट न हो सका। दूसरा जो मसला आसान है वह बयान कर दें।
जवाब : फ़ुक़हा ने मफ़क़ूदुल-ख़बर (खोए हुए व्यक्ति) के मसले में विभिन्न जवाब दिए हैं। इमाम मालिक (रह॰) ने फ़रमाया कि ऐसी सूरत में जब यह विश्वास हो जाए कि अब पति मर गया होगा तो औरत इद्दत की मुद्दत गुज़ारकर दूसरा निकाह कर सकती है। यह विश्वास चार वर्ष में होगा। चार वर्ष में जब यह विश्वास हो जाए तो यह समझा जाएगा कि वह पति अब मर गया और अदालत फ़ैसला करके निकाह ‘फ़स्ख़’ (निरस्त) कर देगी। यहाँ तक कि वह आ भी जाए तो निकाह फ़स्ख़ ही समझा जाए। लेकिन यह इमाम मालिक (रह॰) ने उस समय कहा था जब आने-जाने के साधन बहुत-सीमित थे। इसका तर्क इमाम मालिक (रह॰) की तरफ़ से मालिकी फ़ुक़हा ने यह दिया कि अगर कोई व्यक्ति इस गुम-शुदा आदमी को तलाश करने जाए तो उदाहरणार्थ पूरब में चीन की तरफ़ जाएगा तो छः महीने जाने के लगेंगे और छः महीने आने के लगेंगे। फिर पश्चिम में जाने के लिए छः छः महीने और आने-जाने में लगा देगा और आकर बता देगा कि नहीं मिला। फिर उत्तर और दक्खिन में एक-एक वर्ष लगाएगा। इस तरह चार वर्ष से कम में सही तलाश ही नहीं हो सकती। आजकल के ज़माने में तलाश तुलनात्मक रूप से आसान है। चार वर्ष से कम में यह बात मालूम हो सकती है।
Recent posts
-

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -

फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025