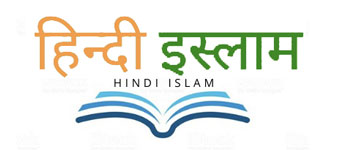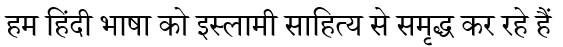फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
-
फ़िक़्ह
- at 26 February 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
आज की चर्चा का शीर्षक है ‘फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े’। इस चर्चा में मौलिक रूप से यह देखना है कि इस्लाम की आरम्भिक सदियों में फ़िक़्हे-इस्लामी के शीर्षक से यह महान कार्य किन परिस्थितियों में और किस तरह अंजाम पाया। किन महानुभावों के हाथों यह कारनामा दुनिया ने देखा और अल्लाह के वे कौन-कौन से बन्दे थे जिन्होंने अल्लाह की कृपा और असीमित सहायता एवं दयालुता से मुस्लिम समाज को आगामी हज़ारों वर्ष के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन संग्रह उपलब्ध कर दिया, जिसका आधार पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल पर था।
इस्लाम में क़ानून और राज्य
दुनिया की तमाम व्यवस्थाओं में और इस्लाम की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और मौलिक अन्तर यह है कि दुनिया के हर क़ानून में राज्य पहले अस्तित्व में आता है और राज्य को चलाने, उसमें अनुशासन क़ायम करने और उसके आन्तरिक एवं बाह्य मामलों को संगठित करने के लिए क़ानून की आवश्यकता बाद में पड़ती है। हर जगह राज्य पहले अस्तित्व में आता है और क़ानून बाद में सामने आता है। राज्य अभीष्ट समझा जाता है और क़ानून इस उद्देश्य की पूर्ति का एक माध्यम और साधन समझा जाता है। इस्लामी व्यवस्था में यह मामला भिन्न है। यहाँ राज्य अपने-आपमें अभीष्ट नहीं है। राज्य एक साधन और माध्यम है अल्लाह के क़ानून को लागू करने का। अल्लाह का क़ानून अपने-आपमें अभीष्ट है। शरीअत पर कार्यान्वयन हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। शरीअत के तमाम पहलुओं के अनुसार जीवन को संगठित करना, यह हर मुसलमान की निजी और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन शरीअत के अनुसार संगठित हो जाएँ, यह मुसलमानों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी भी है और सामूहिक ज़िम्मेदारी भी।
चूँकि इस काम को पूर्ण रूप से और भली-भाँति पूरा करने के लिए राज्य का अस्तित्व ज़रूरी है इसलिए राज्य को बतौर एक साधन और माध्यम के अनिवार्य समझा गया। जैसे-जैसे यह राज्य फैलता गया, जैसे-जैसे इस राज्य को नई-नई समस्याएँ पेश आती गईं, नए-नए इलाक़े फ़त्ह होते गए और जैसे-जैसे नई-नई क़ौमें इस्लाम में दाख़िल होती गईं, उनको नई-नई समस्याएँ और मुश्किलें पेश आती गईं। इन सब समस्याओं का जवाब पवित्र क़ुरआन में और सुन्नते-रसूल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार के साथ या संक्षेप में, स्पष्ट रूप से या सांकेतिक रूप से मौजूद था। जैसे-जैसे नई-नई क़ौमें मुस्लिम समाज का अंग बनती गईं, उनकी पूर्व आस्थाओं, पूर्व धारणाओं और पूर्व विचारधाराओं की शुद्धि एवं सुधार का काम पवित्र क़ुरआन के मार्गदर्शन में शुरू होता गया। इन क़ौमों के पूर्व रिवाज, पूर्व परम्पराएँ, जीवन के प्रति पूर्व धारणाएँ और पूर्व तौर-तरीक़ों में जो बातें सुधार योग्य थीं, उनका सुधार किया गया। और सुधार के बाद उनको इस्लाम की सामूहिक व्यवस्था में इस तरह समो लिया गया कि इससे मुसलमानों की एकता और वैचारिक एकजुटता के लिए कोई समस्याएँ पैदा न हों। यह काम फ़िक़्ह और शरीअत ने भली-भाँति पूरा किया।
मानवता के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी नए अक़ीदे और धर्म को अपना रहे हों और इसके नतीजे में बहुत-सी मुश्किल सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक समस्याएँ पैदा न हो रही हों। जहाँ भी इंसानी आबादी ने बड़ी संख्या में एक व्यवस्था से निकलकर दूसरी व्यवस्था में जीवन व्यतीत करना शुरू किया है, वहाँ हमेशा बहुत-सी अनसुलझी समस्याएँ पैदा हुई हैं। किसी एक क़ानून के दायरे से निकलकर दूसरे क़ानून का दायरा जब भी लोगों की बड़ी संख्या ने अपनाया है इससे अनगिनत मुश्किलें पैदा हुई हैं। मानवता का इतिहास उन मुश्किलों के विवरण से भरा पड़ा है।
यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि इस्लाम के आरम्भिक काल का इतिहास ऐसी किसी जटिल समस्या के विवरण से ख़ाली है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या के इस्लाम में दाख़िल होने के परिणामस्वरूप बहुत जटिल समस्याएँ पैदा हुई हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों जो अपनी समस्याएँ हल न होने की वजह से इस्लाम को छोड़ गए हों। इस्लाम के आरम्भिक काल के इतिहास के रजिस्टर में कहीं नहीं मिलता कि किसी ख़ास इलाक़े में कोई क़ौम या वर्ग ऐसा हो कि उनको उनके अधिकार पूरे तौर पर न मिले हों और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई सामूहिक बग़ावत कर दी हो। राजनैतिक और क्षेत्रीय या जातीय और नस्ली प्रकार की समस्याएँ तो हर दौर में पैदा हुई हैं, और जल्द या देर से उनका समाधान भी तलाश किया जाता रहा। लेकिन यह समस्या कि शरीअत के क़ानून ने इन नए आनेवालों को बराबरी या समानता प्रदान नहीं की या इस्लाम का क़ानून उनकी समस्याएँ सुलझा नहीं सका, यह समस्या कभी पैदा नहीं हुई। यह सब काम कैसे हुआ। इसके लिए क्या उपाय अपनाए गए। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इस्लाम के आदेशों को किस-किस तरह स्पष्ट किया, किन-किन विवरणों को संकलित किया, किन-किन समस्याओं को पहले से भाँप लिया और पहले से उनका हल बता दिया, इन सब सवालों का जवाब और उन मामलों का अध्ययन फ़िक़्हे-इस्लामी की महानता का अनुमान करने के लिए काफ़ी है।
फ़िक़्हे-इस्लामी सहाबा के दौर में
फ़िक़्हे-इस्लामी का आरम्भ और विकास ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ही के शुभ दौर में हो गया था। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के शुभ दौर में पवित्र क़ुरआन अवतरित हो रहा था। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) सुन्नत प्रदान कर रहे थे। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) अपने जीवन पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के अनुसार संगठित कर रहे थे। जिन-जिन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को जितना ज्ञान प्राप्त था उसके हिसाब से वे शरीअत के आदेशों पर विचार भी कर रहे थे। जब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में किसी को ऐसी कोई स्थिति पेश आती थी जिसका समाधान प्रत्यक्ष रूप से पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में मौजूद न हो, और वे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर भी न हों तो वे अपने इज्तिहाद (क़ुरआन और हदीस के गहन अध्ययन से बनी राय) से वक़्ती तौर पर इस समस्या का समाधान भी मालूम कर लेते थे। फिर जैसे ही उनको मौक़ा मिलता था वह समाधान अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में पेश किया जाता था। इस तरह इज्तिहाद की प्रक्रिया अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के मुबारक दौर ही में शुरू हो गई थी। इसलिए हम निस्संकोच यह कह सकते हैं कि फ़िक़्हे-इस्लामी के सर्वप्रथम शिक्षक स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हैं, और फ़िक़्हे-इस्लामी के सर्वप्रथम संस्थापक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) हैं। और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी वे लोग जिनको अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की संगत में शिक्षा और प्रशिक्षण के ज़्यादा अवसर प्राप्त हुए। उनका हिस्सा फ़िक़्हे-इस्लामी के गठन एवं आधारशिला रखने में भी दूसरों से बहुत ज़्यादा है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का मामला शेष तमाम फ़ुक़हा से भिन्न है। बाद में आनेवाले तमाम फ़ुक़हा को और फ़िक़्हे-इस्लामी के छात्रों को शरीअत के स्पष्ट आदेशों से दलील और आदेश लेने और उसूले-इज्तिहाद से काम लेने में बहुत-सी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी जिनकी प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को आवश्यकता नहीं थी।
हमें और आपको अरबी सीखनी पड़ती है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को यह आवश्यकता नहीं थी। हमें और आपको सीरत पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) तो सीरत को स्वयं देख रहे थे और इसका हिस्सा थे। हमें और आपको यह जानना और सीखना पड़ता है कि पवित्र क़ुरआन की कौन-सी आयत किन परिस्थितियों में किस स्थिति में और किस सवाल के जवाब में अवतरित हुई, प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को यह सीखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक ऐसा मौक़ा उपलब्ध था जो बाद में किसी भी इंसान को उपलब्ध नहीं आया। वे ऐसा पत्थर थे जो दूसरे पत्थरों को सोना बनानेवाला था। पारस का यह पत्थर जिन-जिन पत्थरों से लगता रहा है, उनको सोना बनाता गया। जिसमें जितनी प्रतिभाएँ थीं वह इतना ही क़ीमती हीरा बनता गया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) सब-के-सब बिना अपवाद हमारे लिए असाधारण सम्मान और श्रद्धा का स्थान रखते हैं। लेकिन उनके आपस में दर्जों के अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह एक स्पष्ट बात है कि कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का दर्जा बहुत ऊँचा था। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ज्ञान में बहुत नुमायाँ थे। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इस्लाम की समझ एवं अन्तर्दृष्टि और दीन के स्वभाव को समझने में बहुत ऊँचा स्थान रखते थे। यह एक ऐसी स्पष्ट बात है कि जिसके लिए न किसी सुबूत की आवश्यकता है और न कोई विद्वान इससे कोई मतभेद करेगा।
यह कैफ़ियत जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को प्राप्त हुई वह केवल अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को प्रशिक्षण का मौक़ा ज़्यादा मिला। हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) लगभग 61 वर्ष तक अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ रहे। दो वर्ष की उम्र से उनकी अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से निकटता और परिचय था। बहुत बचपन से दोनों में गहरी दोस्ती थी। बचपन दोनों ने साथ गुज़ारा। लड़कपन साथ गुज़ारा। हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के नैतिक आचरण को इतने क़रीब से देखा कि किसी और को यह मौक़ा नहीं मिला। यही वजह है कि वह इस्लाम के पहले दिन से इस्लाम में दाख़िल हुए और 23 वर्ष तक रात-दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ रहे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के रंग में इतना रंग गए कि कभी-कभी अजनबी लोगों को यह शुबा हो जाता था कि शायद यही अल्लाह के रसूल हैं। कई अवसरों पर ऐसा हुआ कि देखनेवालों ने हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अल्लाह के रसूल समझा। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नैतिक गुणों और व्यक्तिगत चरित्र के बारे में वही शब्द प्रयुक्त किए जो इससे पहले अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के लिए प्रयुक्त किए गए थे।
आपको याद होगा कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) पर पहली वह्य आई थी। और वे पहली वह्य के बाद घर तशरीफ़ ले गए और पूरी घटना हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से बयान की तो उन्होंने जवाब में कहा था कि “हरगिज़ नहीं, सर्वोच्च अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख़याल रखते हैं, और लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए अपनी जेब से कमा कर देते हैं। और हक़ के मामलों में आप लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं।” इस तरह के वाक्य हज़रत ख़ुदीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के लिए कहे। इनसे अनुमान होता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) किस प्रकार के गुणों से प्रसिद्ध एवं जाने जाते थे और इस्लाम से पहले ही से उनके उच्च नैतिक आचरण और आदर्श व्यक्तित्व के बारे में मक्का मुकर्रमा के समझदार लोगों की राय क्या थी। बाद में एक प्रसिद्ध अरब सरदार इब्नुद-दुग़ुन्ना ने ठीक यही शब्द हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बारे में कहे। वह उस समय तक मुसलमान नहीं हुआ था। हुआ यों कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को एक मरहले पर अनुमति दी कि अगर क़ुरैश के ज़ुल्मों से पनाह लेकर कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो। सम्भवतः यह भी अभीष्ट था कि मक्का से बाहर जाकर तलाश करें कि दारुल-हिजरत के लिए कौन-सी जगह उचित हो सकती है।
हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) हिजरत के इरादे से मक्का मुकर्रमा से बाहर निकले। अभी आम हिजरत का आरम्भ नहीं हुआ था। यह सम्भवत: छठे या सातवें नबवी वर्ष की बात है। हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) जा रहे थे, रास्ते में एक क़बाइली सरदार मिला, जो अहाबैश का सरदार था। अहाबैश अरब क़बीलों का एक संग्रह था जो मक्का मुकर्रमा के निकट रहते थे। और क़ुरैश से उनके ख़ास तरह के सम्बन्ध थे। अहाबैश का सरदार इब्नुद-दुग़ुन्ना था। वह कहीं सफ़र से वापस आ रहा था। रास्ते में हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को देखा कि तशरीफ़ ले जा रहे हैं। पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी क़ौम ने मुझे परेशान कर दिया है। मेरे लिए अपने रब की इबादत करना असम्भव बना दिया गया है। इसलिए मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे अल्लाह की इबादत करने की आज़ादी हो और कोई मुझे अल्लाह की इबादत से न रोके। बस जहाँ अल्लाह की विस्तृत भूमि में कोई शान्तिपूर्ण जगह शरण के लिए मिलेगी वहाँ चला जाऊँगा।
उसने कहा “हरगिज़ नहीं! सर्वोच्च अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख़याल रखते हैं। और लोगों का बोझ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें अपनी जेब से कमा कर देते हैं। और हक़ के मामलों में सहायता करते हैं।” देखिए ये बिलकुल वही शब्द हैं जो हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने नबी (सल्ल०) के बारे में कहे थे।
इससे आप अनुमान कर लें कि दोनों महानुभावों में नैतिक रूप से कितनी समानता पाई जाती थी। व्यक्तित्वों, किरदार और नैतिक आचरण में कितनी असाधारण समानता थी। यह तो ख़ैर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का सबसे ऊँचा दर्जा था। उनके अलावा शेष प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को भी दर्जा-ब-दर्जा अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के प्रशिक्षण से लाभान्वित होने का मौक़ा मिला। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो इस्लाम के तीन बड़ों में से एक थे, उनका उल्लेख करते हुए एक सहाबी बयान करते हैं कि जब मैं इस्लाम के इरादे से मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में जब हाज़िरी दी तो उनको बहुत अधिक यह फ़रमाते हुए सुना कि मैंने और अबू-बक्र और उमर ने यह किया। मैं और अबू-बक्र और उमर अमुक जगह गए। मैंने और अबू-बक्र और उमर ने यह फ़ैसला किया। इन दोनों का नाम अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की मुबारक ज़बान पर इतना ज़्यादा होता था कि नए आनेवाले लोगों को हैरत होती थी कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि मुहम्मद (सल्ल०) की मुबारक ज़बान से उनका इतना ज़िक्र होता है। बड़े सहाबा की इस नबवी निकटता और प्रशिक्षण का अगर मैं विवरण बयान करने लगूँ तो आज का पूरा दिन शायद नाकाफ़ी हो। इसलिए कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का प्रशिक्षण-स्तर अगर बयान किया जाए तो वह एक लंबी चर्चा का तक़ाज़ा करता है। इसलिए इन उदाहरणों के और अधिक विवरण में नहीं जाऊँगा। बताना यह है कि नबवी प्रशिक्षण से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) लाभान्वित होते थे। और जिस सहाबी में सर्वोच्च अल्लाह ने जितनी प्रतिभा रखी थी उसके हिसाब से उनको इस नबवी प्रशिक्षण की बरकतें और फल मिल रहे थे। फिर सर्वोच्च अल्लाह की तरफ़ से ख़ास प्रबन्ध था, जिसकी वजह से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इस प्रशिक्षण से एक ऐसा कुन्दन बन-बनकर निकल रहे थे जिसका उदाहरण न पहले मिलता है न बाद में मिलता है। न पहले के पैग़म्बरों (अलैहिस्सलाम) को ऐसे साथी मिले न बाद में ऐसे लोगों के आने का कोई सवाल पैदा होता है। यह सर्वोच्च अल्लाह की तरफ़ से विशेष प्रबन्ध था कि जो लोग अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के उत्तराधिकारी बनें और उनके बाद उनके निर्देश और मार्गदर्शन लोगों तक पहुँचाएँ, वे किस दर्जे के लोग होने चाहिएँ। चुनाँचे वे इस दर्जे के लोग थे जिनके चरित्र और व्यक्तित्व की एक झलक अभी आपने देखी। उनमें स्वाभाविक प्रतिभाओं की दृष्टि से इसी तरह का अन्तर था जिस तरह इंसानों में अन्तर होते हैं। उनमें से कुछ, ख़ासतौर पर बदवी पृष्ठभूमि रखनेवाले सहाबा आरम्भ में इतने सीधे-साधे थे कि जब पवित्र क़ुरआन में आया कि रमज़ान में रात के आख़िरी हिस्से में उस समय तक खाने-पीने की अनुमति है जब तक काला धागा सफ़ेद धागे से जुदा न हो जाए तो एक नए-नए मुसलमान होनेवाले बदवी सहाबी यह समझे कि इससे मुराद वे धागे हैं जिससे कपड़ा बुना जाता है। चुनाँचे उन्होंने तकिए के नीचे दो धागे रख लिए और थोड़ी-थोड़ी देर में देखते रहे कि ये अलग होते हैं कि नहीं। सूरज निकल आया लेकिन न उन्होंने अलग होना था और न ही वे अलग हुए। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में इस तरह के सीधे-साधे लोग भी थे। लेकिन जिन लोगों ने आगे चलकर फ़िक़्ह की आधारशिला रखने में हिस्सा लिया और मार्गदर्शन किया, जिनकी मुबारक ज़बान से वे मूल सिद्धान्त और आदेश निकले जिनपर फ़िक़्हे-इस्लामी के आधार है। ये वे लोग थे जो स्वयं प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी अत्यंत श्रेष्ठ और नुमायाँ स्थान रखते थे। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि यह अनुमान हमेशा अनुमान ही रहेगा, जिसका आधार मात्र राय और आन्तरिक राय पर होगी। इसके बारे में निश्चित रूप से तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है अलबत्ता ऐसे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) जिनके फ़तवे संकलित और रिकार्ड होकर बादवालों तक पहुँचे, और जिनकी गणना फ़तवा देने योग्य सहाबा में होती है, उनकी संख्या का अनुमान अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने-क़य्यिम के निकट एक सौ तीस और एक सौ चालीस के दरमियान है।
इन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में से अधिकांश वे लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा आने से पहले से या मदीना मुनव्वरा आने के आरम्भ से अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ थे। उनमें मुहाजिरीन भी शामिल हैं और अंसार भी। मुहाजिरीन का स्थान ज़्यादा नुमायाँ था, क्योंकि वे ज़्यादा समय से नबी (सल्ल०) की संगति में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंसार को केवल दस वर्ष मिले। मुहाजिरीन में ‘साबिक़ूनल-अव्वलून’ (सबसे पहले ईमान लानेवालों) को बीस-बीस और बाईस-बाईस और तेईस-तेईस वर्ष मिले। फिर सबसे बढ़कर जो सम्मान और जो अद्वितीय सुनहरा मौक़ा प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को प्राप्त था वह यह था कि वे वह्य (प्रकाशना) के अवतरण के ज़माने में जी रहे थे। दिन रात उनके सामने क़ुरआन उतर रहा था। उनको मालूम था कि कौन-सी आयत कहाँ अवतरित हुई, किस आयत का क्या अर्थ है। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में एक मौक़े पर कहा था कि “मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इसलिए कि बहुत जल्द ऐसे दिन आएँगे कि तुम पूछोगे लेकिन जवाब देनेवाला कोई नहीं होगा।” ज़ाहिर है क़ुरआन, सीरत और हदीस के बारे में हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बढ़कर कौन बेहतर जवाब दे सकता था। एक बार हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि “मैं पवित्र क़ुरआन की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि यह कहाँ अवतरित हुई, कब अवतरित हुई, किस जगह अवतरित हुई, किन लोगों के बारे में अवतरित हुई। और ख़ुदा की क़सम! अगर मैं जानता कि कोई आदमी मुझसे ज़्यादा किसी आयत का जाननेवाला है तो मैं सवारियों पर सवार होकर महीनों का सफ़र करके जाता और वह ज्ञान प्राप्त कर के आता। लेकिन चूँकि मेरे ज्ञान में ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं।”
चुनाँचे इस तरह के प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) भी मौजूद थे जिनको वह्य के अवतरण के दौर में नबी (सल्ल०) की निगरानी और प्रशिक्षण में जीवन गुज़ारने का मौक़ा मिला। और उनके अन्दर ख़ुद-ब-ख़ुद एक ऐसा प्रशिक्षण पैदा हो गया और वह ज्ञान उनको प्राप्त हो गया कि वह ख़ुद-ब-ख़ुद शरीअत के रंग में रंग गए। शरीअत के स्वभाव से परिचित हो गए और उनकी मुबारक ज़बान से जो आदेश निकलते थे और जो निर्देश निकलते थे, वे सौ प्रतिशत शरीअत के अनुसार होते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जिनके अनुमान और आगे पेश आनेवाले हालात का अनुमान कर लेने की प्रतिभा के अनुसार लगभग सत्रह आयतें अवतरित हुईं। ये सारी की सारी सत्रह आयतें, आदोशों से सम्बन्धित आयतों में से हैं। इससे जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस्लाम के स्वभाव की गहरी समझ का पता चलता है वहाँ उनकी असाधारण और अद्वितीय फ़िक़ही अन्तर्दृष्टि का भी अनुमान होता है।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में चार तरह के लोग थे। कुछ तो आम प्रतिष्ठित सहाबा थे जिनमें वे सब लोग शामिल थे जिन्होंने किसी एक मौक़े पर या दो मौक़ों पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को देखा था। जिनकी आँखों ने अल्लाह के नबी का दीदार किया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में अधिक संख्या तो उन ही लोगों की थी। उसके बाद वे लोग थे जिनको अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में ज़्यादा रहने का मौक़ा मिला। जिन्होंने स्वयं दीन सीखा, दूसरों को सिखाया और बादवालों तक पहुँचाया। उनमें से अधिक संख्या वह है जिनको ‘मुक़ल्लीन’ कहते हैं। यानी थोड़ा बयान करनेवाले। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी-किसी मामले में फ़तवा दिया। कुछ समस्याओं में मार्गदर्शन किया। कुछ हदीसें भी बयान कीं। लेकिन जो सामग्री उनके द्वारा आई है वह थोड़ी है। इसलिए उनको ‘मुक़ल्लीन’ कहते हैं। उनकी संख्या कुछ सौ के लगभग है। इन ही में सौ सवा सौ वे लोग भी हैं जिनके फ़तवे हदीस की किताबों में बिखरे हुए हैं। उनकी एक सूची भी हाफ़िज़ इब्ने-क़य्यिम ने संकलित की है। उनके बाद एक वर्ग ‘मुकस्सिरीन’ का है। यानी जिनसे बड़ी संख्या में या ज़्यादा संख्या में इज्तिहादात और फ़तवे नक़्ल हुए हैं। इन लोगों से भी बड़ी संख्या में हदीसें उल्लिखित हैं, पवित्र क़ुरआन की टीका भी लिखी है और उनके अपने इज्तिहादात भी मिलते हैं, उनके फ़तवे और उनकी अपनी रायें भी मिलती हैं जो क़ुरआन और सुन्नत पर आधारित हैं। इन लोगों से बड़ी संख्या में ये चीज़ें आई हैं। यह ‘मुकस्सिरीन’ कहलाते हैं जिनसे निर्देश बड़ी संख्या में मिले। लेकिन स्वयं उन ‘मुकस्सिरीन’ की संख्या थोड़ी है। उनकी संख्या प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में बीस-पच्चीस से ज़्यादा नहीं है। यह तीसरा वर्ग है।
चौथा और सबसे उच्च और विशिष्ट वर्ग वह है कि जो ‘मुकस्सिरीन’ के भी ‘मुकस्सिरीन’ हैं। ये वे लोग हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ख़ास-ख़ास मैदानों में दक्षता का सर्टिफ़िकेट प्रदान किया। उदाहरण के रूप में एक जगह नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि “सबसे बेहतर क़ुरआन जाननेवाले उबई-बिन-कअब हैं।” एक और जगह फ़रमाया कि “हलाल और हराम का सबसे ज़्यादा ज्ञान रखनेवाले मुआज़-बिन-जबल हैं। यानी जिसको आज फ़िक़्ह कहते हैं — हलाल-हराम के ज्ञान ही को फ़िक़्ह कहते हैं — इसके सबसे बड़े माहिर मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं। एक और जगह फ़रमाया कि “फ़ैसला करने में सबसे ज़्यादा माहिर और जूडिशयल मामलात में सबसे बड़े माहिर अली-बिन-अबी तालिब हैं।” एक और जगह फ़रमाया कि “विरासत और वसीयत के आदेशों के सबसे बड़े माहिर ज़ैद-बिन-साबित हैं।” एक और जगह फ़रमाया कि “अगर तुम क़ुरआन की क़िरअत सीखना चाहते हो तो इब्ने-उम्मे-अब्द की क़िरअत पर क़ुरआन पढ़ो।” इब्ने-उम्मे-अब्द हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद का लक़ब (उपनाम) था जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में बड़ा नुमायाँ स्थान रखते थे। वह प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में इतना बड़ा स्थान रखते थे और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के इतने क़रीब थे कि बाहर से आनेवाले अजनबी उनको नबी (सल्ल०) के परिवार का एक व्यक्ति समझते थे। इतना ज़्यादा अल्लाह के रसूल के घर आया जाया करते थे और उनके निजी मामलों में इतने आगे-आगे रहते थे कि उनकी हैसियत लगभग घर के व्यक्ति की हो गई थी। वह मक्का के बिलकुल आरम्भिक दौर में यानी इस्लाम के दूसरे या तीसरे वर्ष इस्लाम लाए थे। लगभग बीस-इक्कीस वर्ष तक उनको दिन रात नबी (सल्ल०) की सेवा में रहने और हर चीज़ सीखने का मौक़ा मिला।
ज़ाहिर है उनमें जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ‘मुकस्सिरीन’ भी हैं और ‘मुख़स्सिसीन’ भी हैं इन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का इल्म ज़्यादा आम हुआ। बाद में आनेवाले लोगों ने उनसे ज़्यादा सीखा। जो ‘मुक़ल्लीन’ हैं और जिनके मार्गदर्शन से लोगों को सहायता भी तुलनात्मक रूप से कम मिली, उनका ज्ञान भी कम आम हुआ।
कुछ सहाबा वे हैं जो इन ‘मुख़स्सिसीन’ से भी ऊँचा दर्जा रखते हैं। जो किसी एक मैदान के ‘मुख़स्सिस’ नहीं, बल्कि पूरे दीन के ‘मुख़स्सिस’ थे। जैसे चारों ख़लीफ़ा, हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उसमान और हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हुम)। ये वे लोग थे जो लगभग हर मैदान में सबसे नुमायाँ थे और शैख़ैन (हज़रत अबू-बक्र और हज़रत उमर) ख़ास तौर पर। और शैख़ैन में भी ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का स्थान एक दृष्टि से काफ़ी अलग है। इसलिए कि उनका ज़माना ज़रा लंबा है और उनसे लोगों को लाभान्वित होने का मौक़ा ज़्यादा मिला। वे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के दुनिया से जाने के बाद लगभग बारह साढ़े बारह वर्ष ज़िन्दा रहे। इसलिए लोगों ने उनके ज्ञान से ज़्यादा लाभ उठाया।
यही वजह है कि जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) फ़िक़्ह और फ़तवों में ज़्यादा नुमायाँ रहे और जिनसे बड़ी संख्या में ताबिईन ने फ़िक़ही मामलात में लाभ उठाया, उनमें हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का नाम सबसे नुमायाँ है। फ़तवा और राय के मामलात में हदीसों और पवित्र क़ुरआन की आयात से आदेश निकालने में, इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस दर्जे के आदमी हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उनके बारे में फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर-बिन-ख़त्ताब होते। लेकिन चूँकि नुबूवत समाप्त हो गई इसलिए किसी के नबी होने का कोई सवाल नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रतिभाओं, समझ और अन्तर्दृष्टि की दृष्टि से, दीन में गहराई की दृष्टि से और चरित्र और नैतिक आचरण की दृष्टि से वे इस दर्जे के इंसान थे जिस दर्जे के इंसान नबियों में पाए जाया करते थे। और अगर नुबूवत समाप्त न हो गई होती तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी होते।
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को सर्वोच्च अल्लाह ने असाधारण प्रतिभाएँ प्रदान की थीं। उन्होंने पवित्र क़ुरआन का ज्ञान तो प्राप्त किया ही था, इसका विस्तृत विवरण मैं पहले बयान कर चुका हूँ। हदीसों और सुन्नत से उनको कितनी जानकारी थी, उसका विवरण भी कुछ-न-कुछ आ चुका है। पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के आदेशों में गहरी अन्तर्दृष्टि और समझ जितनी उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को प्राप्त थी, अगर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में उनका कोई समकक्ष था तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे और कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उनके ज्ञान की व्यापकता की गवाही दी। उनके बारे में भविष्यवाणी की कि उनके ज्ञान से दुनिया बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी। और अभी मैं बताऊँगा कि आज तक उनके ज्ञान से इतना लाभ प्राप्त किया जा रहा है कि किसी ग़ैर-नबी के ज्ञान और समझ से लाभान्वित होने की कोई शक्ल इससे ज़्यादा सम्भव नहीं है। हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु), जिनको लगभग बारह वर्ष ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का मौक़ा भी मिला, वे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक जीवित रहे और इस पूरे समय में बड़ी संख्या में ताबिईन ने उनसे लाभ उठाया। उनके इज्तिहादात (रायें) और फ़तवे बड़ी संख्या में छोटे सहाबा और उनके ज़रिये ताबिईन तक पहुँचे। हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के दुनिया से जाने के बाद और तीस वर्ष तक नुबूवत के इल्म का नूर फैलाते रहे और लोग बड़ी संख्या में उससे लाभान्वित होते रहे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस दर्जे के इंसान थे कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनी आवश्यकता को क़ुर्बान करके इराक़ के लोगों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ख़ास तौर पर उन्हें कूफ़ा भेजा। वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी यह लगाई गई थी कि वे लोगों के मुक़द्दमों का फ़ैसला किया करें। फ़िक़्ह और शरीअत की शिक्षा दें। और वहाँ एक ऐसी नस्ल तैयार करें जो आगे चलकर इस ज्ञान को फैलाए।
कूफ़ा पहली इस्लामी बस्ती थी जो इराक़ में इस्लाम की विजयों के बाद क़ायम हुई। कूफ़ा और बस्रा सौ प्रतिशत मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। इन दोनों का नक़्शा हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने स्वयं बनाया था। मैंने कई बार टाउन प्लैनिंग के विशेषज्ञों को वह विवरण बताया जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कूफ़ा की बस्ती बसानेवाले सहाबा को बताया था तो उनको बहुत हैरत हुई और कई विशेषज्ञों ने यह माना कि इससे बेहतर नक़्शा आज भी किसी शहर का नहीं है, जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कूफ़ा के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने लकड़ी से रेत में निशानात बनाकर उन्हें समझाया था कि इस तरह शहर बसा लेना। ये दो बस्तियाँ कूफ़ा और बस्रा विभिन्न अरब क़बीलों का संग्रह थीं और नए इस्लामी समाज में इस बात का पहला नमूना थीं कि सौ प्रतिशत इस्लामी बस्तियाँ ऐसी होती हैं। वहाँ चूँकि क़बाइली लोग बड़ी संख्या में जा-जाकर आबाद होने शुरू हो गए थे। ईरानी नव-मुस्लिम भी थे। उनमें से वे भी थे जिन्होंने पहले ज़कात का इनकार किया था और बाद में तौबा करके दोबारा इस्लाम में दाख़िल हो गए थे। ऐसे लोगों के प्रशिक्षण के लिए ख़ास प्रबन्ध की आवश्यकता थी।
इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) को वहाँ भेजा था। जब हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) मदीना मुनव्वरा से कूफ़ा के लिए रवाना होने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनको एक पत्र दिया और कहा कि इस पत्र को वहाँ कूफ़ा की सार्वजनिक सभा में पढ़कर सुनवाया जाए। उसमें लिखा था कि “ऐ कूफ़ावालो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी क़ुर्बानी दे रहा हूँ और अपनी आवश्यकता को क़ुर्बान करते हुए अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मुझे हर वक़्त, हर दिन और हर लम्हा उनसे मश्वरे की आवश्यकता रहती है। और मैं उनके मश्वरे के बिना कोई काम नहीं करता, लेकिन चूँकि तुम्हें एक ऐसे मुअल्लिम (शिक्षक) की आवश्यकता है जो दीन की रूह को समझता हो, इसलिए मैं अपने ऊपर तुम्हें प्राथमिकता देते हुए अबदुल्लाह-बिन-मसऊद को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ।”
यों हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कूफ़ा चले गए। लम्बे समय तक वहाँ ठहरे और वर्षों केवल यह काम किया कि पवित्र क़ुरआन और हदीस की शिक्षा दी, लोगों को प्रशिक्षण दिया कि नए आदेश कैसे निकालें। नए इज्तिहादात (रायों) से लोगों का मार्गदर्शन कैसे करें। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी ‘मुकस्सिरीन’ सहाबा में से थे। उनका जीवन का सारा ज़माना मदीना मुनव्वरा में गुज़रा। उन्होंने लगभग साठ पैंसठ वर्ष तक मदीना मुनव्वरा में यही काम किया। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के आदेशों और इज्तिहादात को लोगों तक पहुँचाया। लोगों का प्रशिक्षण किया कि इन आदेशों से ‘मसाइल’ (व्यावहारिक तरीक़ों) को कैसे निकालें। लोगों को मार्गदर्शन कैसे उपलब्ध करें। वहाँ उन्होंने एक नई नस्ल तैयार की। उन्होंने अपने शिष्यों का एक पूरा दल तैयार कर दिया।
जिस ज़माने में हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) यह काम कर रहे थे, लगभग उसी ज़माने में और क़रीब-क़रीब उतनी ही मुद्दत तक हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) भी मदीना मुनव्वरा में ठहरी रहीं, जो असाधारण और विशिष्ट ज्ञान हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के पास था, वह न केवल ताबिईन, बल्कि स्वयं प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) तक स्थानांतरित करती रहीं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का हलक़ा-ए-दर्स (दीन सिखाने की क्लास) लगा करता था। ताबिईन वहाँ आया करते थे। विभिन्न मामलों में ज्ञान प्राप्त करते थे। नई पेश आनेवाली स्थिति में मसाइल (आदेश) मालूम करते थे और इस तरह एक नस्ल तैयार हो गई जिसने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो दोनों सहाबा के पास जाते थे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास भी जाते थे और हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास भी जाते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि इन दोनों की रायों में मतभेद होता था। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपनी राय पर क़ायम रहते थे और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपनी राय पर क़ायम रहती थीं। इसलिए कि समझ और अन्तर्दृष्टि की दृष्टि से एक व्यक्ति की राय एक और दूसरे की दूसरी हो सकती है।
अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी ऐसे ही ‘मुकस्सिरीन’ सहाबा में से थे। उनका आवास ज़्यादा-तर मक्का मुकर्रमा में रहा। मक्का मुकर्रमा और ताइफ़ में उनके शिष्यों का एक दल तैयार हुआ।
प्रतिष्ठित सहाबा में फ़िक़ही मतभेद और उसके कारण
जैसा कि बताया गया कि विभिन्न इलाक़ों में विभिन्न प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप एक-एक दल तैयार कर दिया। हज़रत उबई-बिन-कअब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने दमिशक़ में, हज़रत ज़ैद-बिन-साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मदीना मुनव्वरा और बस्रा में। इस तरह से हर इलाक़े में एक ऐसी नस्ल तैयार हो गई जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की प्रशिक्षण प्राप्त थी। उनमें से कुछ के पास एक सहाबी से प्राप्त किया हुआ ज्ञान और प्रशिक्षण था। कुछ के पास एक से अधिक सहाबा से प्राप्त किया हुआ प्रशिक्षण था। इस ज्ञान और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उन्होंने शरीअत के आदेशों पर ग़ौर शुरू किया और नए-नए मसाइल (समस्याओं) पर आदेश निकालते गए। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) यह काम अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के ज़माने से कर रहे थे। उनके ज़माने से उनका यह प्रशिक्षण होता चला आ रहा था। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का यह तरीक़ा था कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को जब भी किसी नई स्थिति का सामना होता था, तो अल्लाह के रसूल ही उनकी बात सुनकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दे दिया करते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि एक सहाबी के इज्तिहाद ने उनको ग़लती के रास्ते पर पहुँचा दिया, तो नबी (सल्ल०) उस ग़लती का सुधार कर दिया करते थे। कभी-कभी आंशिक सुधार की आवश्यकता होती थी। नबी (सल्ल०) इस सुधार योग्य भाग का सुधार करके शेष इज्तिहाद की मंज़ूरी दे दिया करते थे। कभी-कभी पूरे इज्तिहाद की मंज़ूरी दे दिया करते थे। इसके उदाहरण हदीस की किताबों में सैंकड़ों हैं। मैं केवल दो उदाहरण पेश करता हूँ।
एक बार प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) किसी लंबे सफ़र पर थे। वहाँ प्रसिद्ध सहाबी हज़रत अम्मार-बिन-यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ग़ुस्ल (स्नान) की आवश्यकता पड़ी। पानी उपलब्ध नहीं था। अब क्या करते। पवित्र क़ुरआन में यह तो लिखा है कि पानी न हो तो वुज़ू कैसे करो। यह स्पष्ट नहीं है कि पानी न हो तो ग़ुस्ल का तक़ाज़ा कैसे पूरा करें। हज़रत अम्मार-बिन-यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इज्तिहाद किया कि अगर वुज़ू का स्थान ‘तयम्मुम’ की प्रक्रिया ले सकती है तो ग़ुस्ल के स्थान पर इससे बढ़कर कुछ और किया जाना चाहिए। वह एक जगह गए जहाँ मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ था। उन्होंने वहाँ जाकर जिस तरह ‘तयम्मुमी ग़ुस्ल’ किया उसके बारे में वे स्वयं ही कहते हैं कि “मैं मिट्टी में इस तरह लोट-पोट हुआ जिस तरह जानवर मिट्टी में लोट-पोट होते हैं।” उन्होंने अत्यन्त दियानतदारी से यह समझा कि ग़ुस्ल की जगह ‘तयम्मुम’ करना हो तो इसी तरह करना चाहिए। जब यह बात अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से बयान की तो उनके मुबारक चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फ़रमाया कि “इसकी आवश्यकता नहीं थी। बस इतना ही ‘तयम्मुम’ काफ़ी था जितना वुज़ू के लिए किया जाता है।” गोया हज़रत अम्मार-बिन-यासिर के ‘तयम्मुम’ के इज्तिहाद को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने नामंज़ूर कर दिया और उसको दुरुस्त क़रार नहीं दिया।
कभी-कभी ऐसा हुआ कि दो सहाबा ने एक जैसी स्थिति में दो विभिन्न रवैये अपनाए। एक सहाबी को नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि तुमने दुरुस्त किया। दूसरे से फ़रमाया कि तुम्हें सुन्नत तरीक़े तक रास्ता मिल गया। यानी दुरुस्त तो दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है। ग़लत एक को भी नहीं कहा। एक को दुरुस्त और दूसरे को सुन्नत के अनुसार क़रार दिया। गोया शरीअत के आदेशों की एक से ज़्यादा व्याख्याएँ सम्भव हैं। कभी-कभी प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने नबी (सल्ल०) के कथनों को दो विभिन्न तरीक़ों से समझा। और उन्होंने एक ही समय में दोनों से फ़रमाया कि “तुमने भी दुरुस्त किया और तुमने भी दुरुस्त किया।” इससे यह पता चला कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात में कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी कार्य या किसी आदेश की एक ही व्याख्या सम्भव होती, तो नबी (सल्ल०) ने एक व्याख्या को दुरुस्त क़रार दिया और शेष के बारे में कहा कि यह दुरुस्त नहीं हैं। कभी-कभी दोनों व्याख्याएँ दुरुस्त क़रार दीं, लेकिन एक को केवल दुरुस्त और दूसरे को सुन्नत के अनुसार क़रार दिया। कभी-कभी दोनों को बराबर दुरुस्त क़रार दिया।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में शरीअत की समझ और राय और इज्तिहाद में जिस अंदाज़ का मतभेद नबी (सल्ल०) के ज़माने में हुआ, उसी अंदाज़ का मतभेद बाद में भी हुआ। इस मतभेद के कारण क्या हैं, उसके कारणों में से कुछ तो वे हैं जो बाद में भी पाए जाते रहे और कुछ वे हैं जो केवल प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के साथ ख़ास थे। उदाहरण के रूप में कुछ कारण वे हैं जो लोगों के व्यक्तित्व और स्वभाव से सम्बन्ध रखते हैं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का स्वभाव और अंदाज़ विभिन्न था। कोई भी दो इंसान अपने स्वभाव और अंदाज़ में एक जैसे नहीं हो सकते। एक को जल्दी ग़ुस्सा आएगा दूसरे को नहीं आता होगा। एक आदमी हर मामले में सब्र से काम लेता होगा, दूसरा नहीं लेता होगा। इस तरह स्वभाव की भिन्नता की मिसालें रोज़ सामने आती हैं। इसका नेकी और बुजु़र्गी से सम्बन्ध नहीं होता। बहुत नेक और मुत्तक़ी (परहेज़गार) इंसान भी कभी-कभी सब्र का दामन छोड़ देता है। इसके विपरीत कभी-कभी बहुत गुनाहगार इंसान बहुत सब्र से काम ले लेता है। अत: इन चीज़ों का सम्बन्ध लोगों के स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति से होता है, किसी की नेकी और बुजु़र्गी से नहीं होता, बल्कि इंसान की उस बनावट से होता है जो सर्वोच्च अल्लाह ने रखी है। स्वभाव के इस अन्तर और तबीअतों के इस अन्तर की वजह से कभी-कभी एक मामले को समझने में और उसकी व्याख्या में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में अन्तर पैदा हो जाया करता था। इसके उदाहरण आगे आ रहे हैं।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और प्रतिष्ठित फ़ुक़हा में मतभेद का दूसरा कारण यह था कि पवित्र क़ुरआन ने कुछ जगह कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त किए हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। अरबी भाषा में उनका अर्थ एक से अधिक है। पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है, “जिन औरतों को तलाक़ हो जाए वे तीन ‘क़ुरू’ तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद चाहें तो दूसरा निकाह कर सकती हैं।” अब ‘क़ुरू’ से क्या मुराद है। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का ख़याल था कि इससे मुराद वह संक्षिप्त मुद्दत है जो हर महीने में तीन या चार या पाँच छः दिन होती है। जिसमें महिलाओं को नमाज़ माफ़ हो जाया करती है। कुछ ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने समझा कि इससे मुराद उसके अलावा वह शेष मुद्दत है जो पाकीज़गी की मुद्दत कहलाती है। अब चूँकि अरबी भाषा में इस शब्द के दोनों अर्थ प्रयुक्त होते हैं इसलिए प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और फ़ुक़हा ने अपनी-अपनी समझ से किसी एक अर्थ को निर्धारित करने की कोशिश की। अब इन दोनों अर्थों की वजह से दो विभिन्न अर्थ इस आयत के सामने आ जाएँगे। इन दो टीकाओं की वजह से दो तरह के आदेश सामने आ जाएँगे।
कभी-कभी किसी सुन्नत के आदेश को या किसी हदीस को प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने दो अंदाज़ से समझा, और जिसने जिस अंदाज़ से समझा उसने उस अंदाज़ से उसपर अमल किया। समझने में या तो यह स्थिति पेश आई कि अरबी भाषा की दृष्टि से उस आदेश के समझने में एक से अधिक दृष्टिकोण से समझने की गुंजाइश मौजूद थी। या अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक बात को दो विभिन्न अवसरों पर कहा। एक बार एक शैली अपनाई, दूसरी बार दूसरी शैली अपनाई। जिस सहाबी ने एक शैली को याद रखा उन्होंने एक अंदाज़ से इसका अर्थ लिया। जिस सहाबी ने दूसरी शैली को याद रखा उन्होंने दूसरे अंदाज़ से इसकी व्याख्या की। इस तरह से दो दृष्टिकोण सामने आ गए। कभी-कभी ऐसा हुआ कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की अपनी अन्तर्दृष्टि और समझ के अनुसार पवित्र क़ुरआन की किसी आयत या सुन्नत के दो विभिन्न अर्थ हो सकते थे। इस वजह से उनकी राय का मतभेद हुआ।
कभी-कभी प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में यह मतभेद भी पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कोई बात बताई थी या नहीं। अगर बताई थी तो किस सन्दर्भ में बताई थी। उदाहरण के रूप में एक महिला ने आकर यह गवाही दी कि मेरे पति का देहान्त हुआ था तो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने मेरे लिए न किसी नफ़क़े (गुज़ारा भत्ता) का आदेश दिया था न आवास का प्रबन्ध अनिवार्य क़रार दिया था। इसपर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सहाबा की मौजूदगी में फ़रमाया कि “हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को एक महिला के बयान के आधार पर नहीं छोड़ सकते जिसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको याद रहा या भूल गई।” हालाँकि वह महिला सहाबिया हदीस बयान कर रही थीं। लेकिन यह राय का एक मतभेद है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इससे इत्तिफ़ाक़ नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़ैसला किया कि लोगों में ज़्यादा मह्र अदा करने की नीति पैदा हो गई है। उन्होंने इस रुजहान को हतोत्साहित करने का फ़ैसला किया और एक दिन मस्जिदे-नबवी में तक़रीर करते हुए एलान किया कि मैंने तय किया है कि आज के बाद मह्र की ज़्यादा-से-ज़्यादा हद नियुक्त की जाए और इससे ज़्यादा मह्र नियुक्त करने का किसी अधिकार न हो। मस्जिद में बहुत-से सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी ने इससे मतभेद नहीं किया। किसी सहाबी के ज़ेहन में इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं आई। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने देखा कि एक बूढ़ी महिला आ रही थीं। उनका नाम सम्भवत: हज़रत ख़ौला था। उन्होंने पूछा कि मैंने यह बात सुनी है, क्या तुमने मह्र की ज़्यादा-से-ज़्यादा हद नियुक्त करने की बात की है? हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि “हाँ, मैंने कहा है!” महिला ने कहा कि “तुम्हें किसने यह हक़ दिया है? क़ुरआन हकीम में तो आया है कि ‘अगर तुमने उन्हें सोने चाँदी का ढेर भी दिया है तो वापस मत लो।’ तो क़ुरआन तो ढेर तक देने की बात करता है। जहाँ ढेर देने की गुंजाइश हो तो तुम एक हद से ज़्यादा मह्र देने पर कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हो?”
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने तमाम सहाबा को दोबारा जमा किया और फ़रमाया कि “उमर ने ग़लत कहा और इस महिला ने दुरुस्त कहा। मैं अपना फ़ैसला वापस लेता हूँ और मुझे मह्र की हदबंदी करने का कोई अधिकार नहीं।” यह गोया राय और समझ का मतभेद हो सकता है। इसमें यह कहना कि किस सहाबी की राय दुरुस्त है या किसकी राय दुरुस्त नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। ये सब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ही की विभिन्न रायें थीं। उनमें से बाद में आनेवाले फ़ुक़हा ने अपनी-अपनी अन्तर्दृष्टि और तर्कों के अनुसार लिया और लाभ उठाया।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की रायों में मतभेद का एक बड़ा कारण यह था कि कभी-कभी परिस्थितियों के परिवर्तन से एक सहाबी ने यह समझा कि पवित्र क़ुरआन या सुन्नत में जो आदेश दिया गया है वह इन परिस्थितियों पर चस्पाँ नहीं होता। अत: इन परिस्थितियों में इस आदेश पर अमल नहीं किया जाएगा। कुछ और सहाबा ने समझा कि नहीं इन परिस्थितियों में भी इस आदेश पर अमल किया जाएगा। यह एक subjective राय है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन में जहाँ मसारिफ़े-ज़कात (ज़कात की मदों) का आदेश है वहाँ फ़रमाया गया है कि “ये सदक़ात तो फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए हैं” (क़ुरआन, 9:60), वहाँ आया है कि “....उन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है जिनके दिलों को नर्म करना अभीष्ट हो।” यानी उन लोगों को जो इस्लाम के दुश्मन हों और यह उम्मीद हो कि अगर उनको कुछ भौतिक संसाधन उपलब्ध कर दिए जाएँ तो उनकी दुश्मनी में कमी आ जाएगी। या इस्लाम और कुफ़्र की सीमा पर दरमियान में खड़े हों और यह ख़याल हो कि अगर उनकी आर्थिक समस्याएँ कुछ कम कर दी जाएँ तो ये इस्लाम में दाख़िल हो जाएँगे। या इस्लाम में दाख़िल तो हो गए हैं, लेकिन अभी ईमान में दृढ़ता और व्यवहार में स्थायित्व नहीं आया और यह प्रबल सम्भावना है कि अगर उन लोगों को आर्थिक संसाधन दे दिए जाएँ और वेतन बाँध दिया जाए, आर्थिक सहायता की जाए तो इस्लाम में और दृढ़ हो जाएँगे। इस तरह के लोगों के लिए ‘मुअल्लफ़तुल-क़ुलूब’ (दिलों को नर्म करना) की शब्दावली प्रयुक्त की गई है और उनको ज़कात की मद से रक़म देने की गुंजाइश रखी गई है। ‘मुअल्लफ़तुल-क़ुलूब’ के लिए कमज़ोर, मुहताज या ग़रीब होना ज़रूरी नहीं। ग़रीब तो फ़क़ीरों और मिस्कीनों में आ गए। ‘मुल्लफ़तुल-क़ुलूब’ अगर संसाधन युक्त भी हों और उनके दिलों को नर्म करना दरकार हो तो उनको ज़कात की मद से पैसे दिए जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने मुबारक ज़माने में कुछ अरब क़बीलों के सरदारों को, जो अरब के बहुत प्रभावशाली सरदार थे, जो अगर इस्लाम के विरोध में जमे रहते तो मुसलमानों को बहुत नुक़्सान पहुँचा सकते थे और उन्हें परेशान कर सकते थे। उनकी इस्लाम-दुश्मनी को कम करने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने काफ़ी समय से ज़कात की रक़म से कुछ मद नियुक्त कर दी थी जो उन सरदारों को हर साल मिलती थी। नबी (सल्ल०) के मुबारक दौर में और बाद में हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में यह रक़म नियमित रूप से उनको मिलती रही। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के आरम्भिक काल में भी कुछ वर्षों तक मिलती रही। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में विजयों का दायरा विस्तृत हुआ और अरब में इस्लाम लगभग सौ प्रतिशत फैल गया तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इन क़बाइली सरदारों की यह मदद बन्द कर दी और फ़रमाया कि अब इस्लाम तुम्हारा मुहताज नहीं रहा। अब तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़ुदा-न-ख़ास्ता ‘मुअल्लफ़तुल-क़ुलूब’ की मद निरस्त नहीं की। पवित्र क़ुरआन के किसी आदेश को निष्क्रय नहीं किया, बल्कि यह देखा कि इस नई स्थिति पर पवित्र क़ुरआन का आदेश चस्पाँ होता है कि नहीं होता। बात को समझाने के लिए इतना कहता हूँ कि उदाहरण के रूप में अगर मैं यह कहूँ कि मुझे ‘तालीफ़े-क़ल्ब’ (दिल को मोहने) के लिए ज़कात से पैसे दिए जाएँ, इसलिए कि अगर मुझे मुअल्लफ़तुल-क़ुलूब की मद से पैसे न दिए गए तो मैं ख़ुदा-न-ख़ासता इस्लाम को नुक़्सान पहुँचाऊँगा। और आप सब कहें कि नहीं तुम्हें ‘मुल्लफ़तुल-क़ुलूब’ की मद में ज़कात की रक़म से पैसे नहीं मिलने चाहिएँ। तो यह एक राय है और निश्चय ही दुरुस्त राय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने ‘मुअल्लफ़तुल- क़ुलूब’ की मद ही समाप्त कर दी, बल्कि यह कहा जाएगा कि आपने इस मद से मेरी entitlement या पात्रता को स्वीकार नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह तय किया कि इन लोगों की entitlement और admissibility या पात्रता को परिस्थितियों के बदल जाने की वजह से समाप्त कर दिया। इसलिए कि अब वे परिस्थितियाँ नहीं रहीं। कुछ और सहाबा का कहना था कि नहीं अब भी देना चाहिए। यह एक मतभेद है जो परिस्थितियों के बदलने और अपेक्षाओं के विभिन्न हो जाने की वजह से पैदा हुआ। इस तरह के मतभेद के कारण बाद में भी मौजूद रहेंगे। आज भी हैं और अतीत में भी थे।
फ़िक़्हे-इस्लामी पर प्रतिष्ठित सहाबा के स्वभाव और रुचि में मतभेद का प्रभाव
एक और बड़ा कारण यह है जिसकी तरफ़ मैं पहले इशारा कर चुका हूँ। वह व्यक्तिगत रूप से लोगों के स्वभाव और प्रवृत्ति का मामला है। मानव स्वभाव और ज़ेहन में एक विविधता पाई जाती है। कुछ लोग हैं जो अत्यन्त बौद्धिक स्वभाव रखते हैं और हर चीज़ को बुद्धि के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव विशुद्ध रूप से भावनात्मक होता है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) मस्जिदे-नबवी में ख़ुतबा (अभिभाषण) दे रहे थे। कुछ लोग खड़े थे। कुछ लोग बैठे थे। कुछ लोग अभी गली में थे और मस्जिद की तरफ़ आ रहे थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ख़ुतबा जब शुरू करने लगे तो फ़रमाया कि जो खड़े हैं वे बैठ जाएँ। एक सहाबी जो अभी गली में थे, वे वहीं पर बैठ गए। कुछ लोग जो मस्जिद की तरफ़ आ रहे थे, वे नहीं बैठे और मस्जिद की तरफ़ चलते रहे। जो चलते रहे उन्होंने इस आदेश को एक बौद्धिक रूप से देखा। बौद्धिक व्याख्या यह की कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का कथन उन लोगों के लिए है जो मस्जिदे-नबवी में दाख़िल हो चुके हैं। जो लोग अभी मस्जिद में दाख़िल नहीं हुए उनके लिए यह कथन नहीं है। यह एक बौद्धिक व्याख्या है जिसकी वजह से वे चलते रहे। जो लोग बैठ गए थे उनकी व्याख्या भावनात्मक थी कि जनाब बैठने का आदेश है तो बस बैठ जाएँ और खड़े होने का आदेश है तो खड़े हो जाएँ। यह भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) की तरफ़ से जो आदेश मिले उसपर बिना ना-नुकुर किए अमल किया जाए। यह अपनी जगह एक शान रखनेवाली व्याख्या है और इस दूसरी व्याख्या की अपनी एक शान है। दोनों में से एक दृष्टिकोण को दुरुस्त और दूसरे को ग़लत क़रार देना बहुत मुश्किल है। यह इंसान के स्वभाव और समझ पर निर्भर है। अपनी तबीअत और अपनी प्रवृत्ति पर है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की प्रवृत्ति होगी वह उस तरह करेगा। यह विविधताएँ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के स्वभाव में भी थीं। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का स्वभाव बड़ा बौद्धिक था। कुछ सहाबा का स्वभाव बड़ा भावनात्मक था। कुछ सहाबा के स्वभाव में दोनों पहलू थे।
इस्लाम किसी की रुचि और स्वभाव को दबाता नहीं है। यह इसलिए नहीं आया कि आपके ज़ौक़ को दबादे, या किसी के स्वभाव को बदल दे जो अल्लाह ने बनाया है। स्वभाव में अगर कोई चीज़ शरीअत से टकराती हो तो बदलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ शरीअत से टकराती नहीं है तो शरीअत को उसे ज़बरदस्ती बदलना पसंद नहीं करती। दूसरी चीज़ों तो बात ही क्या, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को तो अपने रुचि की पैरवी का भी पाबंद नहीं बनाया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) पूछते थे कि यह आपका मश्वरा है या शरीअत का आदेश है। और बहुत बार यह हुआ है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि यह शरीअत का आदेश नहीं, बल्कि मेरा निजी मश्वरा है। ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की निजी इच्छा के बावजूद कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने उनके निजी मश्वरे से मतभेद किया। एक महिला बरीरा का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है जिन्होंने अपने निजी मामले में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के व्यक्तिगत मश्वरे से मतभेद किया।
इस तरह के कुछ मामलात हैं जिनका फ़ैसला आदमी अपनी रुचि से करता है। अपनी निजी पसंद-ना-पसंद से करता है। इसमें कभी-कभी किसी दूसरे आदमी के मश्वरे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। फिर विभिन्न इंसानों के स्वभाव और रवैये विभिन्न होते हैं। गर्म इलाक़ों के लोगों का स्वभाव और होता है। मरुस्थली इलाक़ों के लोगों का स्वभाव और होता है और पर्वतीय क्षेत्रों के रहनेवाले लोगों का स्वभाव और होता है। बड़े विकसित और सभ्य स्थानों के लोगों का स्वभाव और होता है। स्वभावों के परिवर्तन के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें भौगोलिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। ये सारी विविधताएँ इंसानों की विविधताएँ हैं, जिनको पवित्र क़ुरआन ने अल्लाह की निशानियाँ क़रार दिया है। “और उसकी निशानियों में से है आकाशों और धरती का सृजन और तुम्हारी भाषाओं और रंगों की विविधता भी है।” (क़ुरआन, 30:22) अत: इस विविधता और रंगा-रंगी को तो क़ुरआन बरक़रार रखता है और इसको मिटाने का आदेश नहीं देता है।
जब यह विविधता और अन्तर होगा, तो इसका प्रभाव लोगों की समझ पर भी पड़ेगा। जब समझ पर पड़ेगा तो राय विभिन्न होगी, इज्तिहादात विभिन्न होंगे। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में इसके अनगिनत उदाहरण हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके बेटे अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के स्वभावों में ज़मीन-आसमान का अन्तर था। पिता का स्वभाव अत्यन्त बौद्धिक और बेटे का स्वभाव अत्यन्त समर्पणवाला। अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जब मदीना मुनव्वरा से कहीं, विशेषकर मक्का मुकर्रमा के सफ़र पर जाते थे तो उसी रास्ते को अपनाते थे जो नबी (सल्ल०) ने अपनाया था। जहाँ नबी (सल्ल०) ने पड़ाव किया, वहाँ अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी पड़ाव करते थे। यहाँ तक कि अगर नबी (सल्ल०) रास्ते में कहीं शौच के लिए बैठे होते तो अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी बैठ जाते थे, आवश्यकता हो या न हो। ज़ाहिर है, इस्लाम ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। यह चीज़ इस्लाम में न सुन्नत है, न मुस्तहब है न कुछ और है। लेकिन अगर कोई प्रेम से उन ख़ालिस निजी और व्यक्तिगत चीज़ों में भी नबी (सल्ल०) की पैरवी करता है तो वह उसके समर्पणभाव वाले स्वभाव की दलील है। जो व्यक्ति ऐसे समर्पणभाव का रवैया अपनाता है तो सर्वोच्च अल्लाह उसका अज्र देगा, लेकिन यह रवैया हर इंसान से शरई तौर पर दरकार नहीं है। इंसानों को इसका आदेश नहीं दिया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कभी ऐसा नहीं किया। वे तो एक बार सफ़र पर जा रहे थे तो देखा कि लोग उस वृक्ष की तलाश में थे जहाँ बैठकर नबी (सल्ल०) ने सहाबा से बैअत ली थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने पूछा क्यों तलाश कर रहे हो। किसी ने कहा उसके नीचे नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा, “यह तो बड़ी ख़तरनाक बात है। लोग आज उसके नीचे नमाज़ पढ़ेंगे। परसों उसको चूमेंगे। इसके बाद तबर्रुक लेकर जाएँगे।” उन्होंने उसके काटने का आदेश दे दिया। अब यह एक अत्यन्त बौद्धिक ढंग है जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही समझ सकते थे कि पाँच सौ वर्ष बाद क्या होगा। शायद कोई और होता तो न समझता।
हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने तक रौज़ा मुबारक का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला रहता था, जहाँ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का मज़ार मुबारक है, वह वास्तव में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का मकान है। यह तो सबको मालूम है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का जो मकान था वह एक लंबे साइज़ के प्लाट पर था। उसमें ज़रा चतुर्भुज प्रकार का कमरा और एक छोटा-सा सेहन था। इस सेहन का दरवाज़ा बाहर एक तंग-सी गली में खुलता था और इधर एक कमरा और एक छोटा-सा खिड़की नुमा दरवाज़ा था, जिसमें आदमी झुककर जाता हो, वह मस्जिदे-नबवी में खुलता था। इस तरह के दरवाज़े को अरबी में ‘ख़ूख़ा’ कहते हैं। जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का देहान्त हो गया, तो इस हिस्से में उनको दफ़न किया गया। बाद में हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ को भी उसी कमरे में दफ़न किया गया जो हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के घर का कमरा था। गोया उनके बेडरूम में दोनों क़ब्रें थीं। जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का देहान्त हुआ और वह भी वहाँ पर दफ़न हुए तो हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने सोचा कि अब यहाँ एक नामहरम का मज़ार है और मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए। आप देखें कि तक़्वा और शर्म-हया की इन्तिहा है। चुनाँचे अब उन्होंने एक दीवार बनाकर उस कमरे के दो हिस्से कर दिए और लोगों की सुविधा की ख़ातिर बाहर गली में इसका छोटा दरवाज़ा खोल दिया। उधर से दीवार लगाकर बंद कर दिया और गली में एक छोटा-सा दरवाज़ा खोल दिया। लोग वहाँ से आया करते थे और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की क़ब्र की ज़ियारत (दर्शन) करके और सलाम पढ़कर चले जाते थे। हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने ज़माने में एक रोज़ क़ब्र पर सलाम के लिए हाज़िर हुए तो देखा कि एक साहिब क़ब्रे-मुबारक पर झुके हुए हैं और वहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। पहले तो वह व्यक्ति बताना नहीं चाहता था। लेकिन हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के आग्रह करने पर उसने बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और नबी (सल्ल०) की क़ब्र मुबारक की मिट्टी तबर्रुक के तौर पर ले जाना चाहता हूँ। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उस व्यक्ति से मिट्टी वापस ली या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाद में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के मश्वरे से इस दरवाज़े को बंद करा दिया। केवल एक छोटी-सी खिड़की खुलवा दी कि लोग बाहर से क़ब्र मुबारक देख सकें और सलाम पढ़ सकें और अन्दर दाख़िल होने की अनुमति न हो। वह दिन और आज का दिन कोई व्यक्ति मुबारक हुजरे में दाख़िल नहीं हुआ। वह दीवार कभी नहीं खुली। उसके बाद से बंद हो गई। हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) का यह फ़ैसला बज़ाहिर उस दूसरे ज़ाइर (श्रद्धालु) के मुहब्बत में दीवानगीवाले स्वभाव से बहुत विभिन्न था। सम्भव है कि इससे सिलसिले में जनाधार मालूम किया जाता तो अधिकतर लोग कहते कि नहीं भई क़ब्र मुबारक को चूमने का मौक़ा मिलना चाहिए। लेकिन हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़ेहन में वे तमाम परिणाम थे जो भविष्य में निकल सकते थे। उन्होंने इस चीज़ की अनुमति नहीं दी।
इस तरह से विभिन्न स्वभावों और प्रवृत्तियों के अन्तर की वजह से विभिन्न प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने विभिन्न ढंग से इज्तिहाद किया। जब विभिन्न ढंग से इज्तिहाद किया तो इससे विभिन्न प्रकार के आदेश सामने आए। एक तरफ़ हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं और एक तरफ़ हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं। एक तरफ़ हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं जो हमेशा कोशिश करते थे कि उन्हें किसी मसले में अपनी राय क़ायम ही न करनी पड़े, बल्कि इसकी नौबत ही न आने देते थे और कोशिश करते थे कि जिस तरह से सुना है उसी तरह से बयान कर दें। या बड़े सहाबा से जो सुना वह बयान कर दें। इस तरह उनकी कुछ रायें ऐसी हो गईं जो आम सहाबा की रायों से भिन्न थीं। जिसको आप ‘शुज़ूज़’ (अपवाद) कह सकते हैं यानी ‘शाज़ राय’ (अपवाद मत)।
ये तीनों प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) तीन विभिन्न विशेषताएँ रखते थे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) जिनके रवैये में थोड़ा-सा खुलापन था। मैं अंग्रेज़ी का शब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहता, लेकिन समझाने की ग़रज़ से कह रहा हूँ कि उनका रवैया थोड़ा सा liberal था। यानी उनके इज्तिहाद के अंदाज़ में एक खुलापन था। कुछ मामलों में जहाँ शेष सहाबा की राय ज़रा मुश्किल होती थी, वे आसान इज्तिहाद किया करते थे और आसान समाधान पेश करते थे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का रवैया इस मामले में बड़ी सख़्ती का था। उनके इज्तिहादात और फ़तवे बड़े सख़्त होते थे। उनकी कोशिश सम्भवतः यह होती थी कि कोई ऐसी सम्भावना न रहे कि शरीअत के किसी आदेश का उल्लंघन हो, बल्कि जो सबसे कठिन रास्ता हो उसी को अपनाया जाए। आसान रास्ते में सम्भावना है कि ग़लत हो, मुश्किल रास्ते में इसकी सम्भावना कम है। सहाबा और ताबिईन में प्रसिद्ध था कि हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सख़्तियाँ, हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ‘शुज़ूज़’ और हज़रत अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रुख़्सत प्रसिद्ध हैं यानी उनकी रुख़्सतें और आसान रायें।
इन उदाहरणों से यह अनुमान हो गया होगा कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में, ताबिईन में, तबा-ताबिईन में फ़क़ीह या मुज्तहिद के इज्तिहाद पर उसके स्वभाव के अन्तर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले उसकी क़ुरआन की समझ की वजह से, फिर सुन्नत की समझ की वजह से, फिर अपनी निजी राय के अलग होने की वजह से, फिर अपने स्वभाव और प्रवृत्ति की वजह से, फिर परिस्थितियों के बदलने और स्थिति के तबदील होने से और फिर उस इलाक़े और माहौल से जहाँ बैठकर वह इज्तिहाद कर रहा है। यह मतभेद प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने से आना शुरू हुआ। ताबिईन के ज़माने में भी जारी रहा। फ़िक़्हे-इस्लामी ताबिईन के दौर में
ताबिईन की संख्या प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है। जो ताबिईन दीन की समझ में नुमायाँ हुए उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। लेकिन ताबिईन में सात प्रतिष्ठित फ़ुक़हा बहुत नुमायाँ हुए जो ‘फ़ुक़हा-ए-सबआ’ कहलाते हैं, यानी सात बड़े फ़ुक़हा। अक्सर और अधिकतर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के तमाम उलूम और इज्तिहादात इन सात फ़ुक़हा तक पहुँचे और उनके इज्तिहादात के ज़रिये वे आगे तबा-ताबिईन तक पहुँचे। इन सात बड़े ताबिईन फ़ुक़हा में यह बयान करना तो बहुत मुश्किल है कि क्रम में पहले कौन है और बाद में कौन। इसलिए कि ताबिईन के दर्जात के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। उनके नाम बिना क्रम के ये हैं।
1. हज़रत क़ासिम-बिन-अबदुल्लाह-बिन-अबी-बक्र, यह हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पोते थे। उन्होंने अपनी फूफी हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से एक लम्बे समय तक ज्ञान प्राप्त किया। ज़ाहिर है कि हज़रत उम्मुल-मोमनीन (रज़ियल्लाहु अन्हा) के भतीजे और महरम थे तो बे-तकल्लुफ़ हर वक़्त आ जा सकते थे। इसलिए दूसरों की तुलना में उनका ज़्यादा समय हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के यहाँ गुज़रा। उन्हें लगभग बीस-बाईस वर्ष उम्मुल-मोमनीन के साए में प्रशिक्षण पाने का मौक़ा मिला। जिस अंदाज़ से उनको ज्ञान प्राप्त करने का मौक़ा मिला होगा वह शेष लोगों को नहीं मिला होगा। उम्मुल-मोमिनीन के अलावा उनको हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से भी भरपूर लाभ उठाने का मौक़ा मिला।
2. हज़रत सईद-बिन-मुसय्यिब, जो हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शिष्य भी थे, दामाद भी थे और एक लम्बे समय तक यानी लगभग तीस-पैंतीस वर्ष तक उनको हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास रहने का मौक़ा मिला। ज़ाहिर है कि जो आदमी इतना क़रीबी शिष्य हो और बाद में दामाद भी बन जाए, उसको जो निकटता प्राप्त होगी वह शेष लोगों को प्राप्त नहीं होगी। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अलावा उन्होंने मदीना मुनव्वरा के दूसरे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से भी भरपूर ज्ञान प्राप्त किया।
3. हज़रत सुलैमान-बिन-यसार, यह उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) के ख़ास पालक और प्रशिक्षण प्राप्त थे। उनके अलावा मदीना मुनव्वरा के अनेक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से ज्ञान प्राप्त किया जिनमें हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा), हज़रत ज़ैद-बिन-साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसे बड़े सहाबा शामिल थे।
4. हज़रत ख़ारिजा-बिन-ज़ैद-बिन-साबित, यह उन ही हज़रत ज़ैद के बेटे हैं जिनके बारे में नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया था कि “सबसे ज़्यादा विरासत का ज्ञान रखनेवाले ज़ैद हैं। उन्होंने लगभग चौथाई सदी तक अपने पिता और दूसरे बड़े सहाबा से फ़िक़्ह और इज्तिहाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
5. हज़रत उर्वा-बिन-ज़ुबैर-बिन-अव्वाम : हज़रत ज़ुबैर-बिन-अवाम जो अशरा-मुबश्शरा (वे दस सहाबी जिनके जन्नती होने की ख़ुशख़बरी उन्हें उनकी ज़िन्दगी में ही सुना दी गई थी) में से हैं, उनके बेट। हज़रत उर्वा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के भांजे थे। वे और क़ासिम-बिन-मुहम्मद हमदर्स (सहपाठी) भी थे और गहरे दोस्त भी। ज़ाहिर है एक भांजा था, एक भतीजा था, और दोनों को हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने प्रशिक्षण दिया। हज़रत उर्वा सीरतुन्नबी पर सबसे पहली किताब लिखनेवाले विद्वान हैं। और यह ताबिईन में जीवनी के सबसे बड़े माहिर समझे जाते थे। उर्वा ने दूसरे बहुत-से बड़े सहाबा से भी ज्ञान प्राप्त किया जिनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ नाम स्वयं उनके प्रतिष्ठित पिता हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का है।
6. हज़रत अबैदुल्लाह-बिन-अब्दुल्लाह-बिन-उत्बा-बिन-मसऊद : यह उक़बा-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) सहाबी के पोते थे।
7. सातवें फ़क़ीह के बारे में ज़रा मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सालिम-बिन-अब्दुल्लाह-बिन-उमर हैं। कुछ और लोगों का कहना है कि नहीं कुछ और लोग हैं।
ये ‘फ़ुक़हा-ए-सबआ’ कहलाते हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की बड़ी संख्या से ज्ञान प्राप्त किया। उनके इज्तिहादात को इकट्ठा किया, लिखित रूप में संकलित किया और लम्बे समय तक उनकी शिक्षा दी।
इनके अलावा जो ताबिईन नुमायाँ थे, उनमें भी कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हैं।
1. हज़रत अता-बिन-अबी-रिबाह, जो मक्का मुकर्रमा में लम्बे समय तक रहे और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से ज्ञान प्राप्त किया।
2. मुहम्मद-बिन-मुस्लिम-बिन-शहाब ज़ोहरी, जो मदीना मुनव्वरा में लम्बे समय रहे और इमाम मालिक (रह॰) के उस्तादों (गुरुओं) में हैं।
3. हज़रत इमाम नाफ़े जो मदीना मुनव्वरा में रहे और अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शागिर्द (शिष्य) और इमाम मालिक (रह॰) के उस्तादों में हैं।
इन तमाम ताबिईन ने विभिन्न इलाक़ों में विभिन्न शहरों में जीवनियाँ गुज़ारीं और सहाबा से जो कुछ जैसे सीखा था वह कुछ वैसे ही आगे दूसरों तक पहुँचाते गए। ये लोग नए आनेवाली समस्याओं का जवाब भी दिया करते थे। नई स्थिति में लोगों का मार्गदर्शन भी किया करते थे। इस तरह जिन-जिन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के शिष्य जिन-जिन इलाक़ों में ठहरे रहे उन इलाक़ों में इस सहाबी के इज्तिहाद की शैली प्रचलित हो गई।
कूफ़ा का उदाहरण लें। वहाँ हज़रत अली-बिन-अबी तालिब और हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने लम्बा समय गुज़ारा। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तो शहादत भी कूफ़ा ही में हुई। कूफ़ा में जिन ताबिईन ने इन दोनों सहाबा से ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने उसके आधार पर एक ऐसी ख़ास शैली और मन्हज को जन्म दिया जो इन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात की रौशनी में संकलित हुआ था। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) मदीना मुनव्वरा में रहे। इन दोनों लोगों का अपना-अपना ख़ास मन्हज (शैली) था। हज़रत अबू-हुरैरा के यहाँ रिवायतें (उल्लेख) ज़्यादा थीं हज़रत अबदुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के स्वभाव में सख़्ती थी और उनकी सख़्तियाँ प्रसिद्ध थीं। उनसे जिन ताबिईन ने ज्ञान प्राप्त किया उनमें इमाम नाफ़े ज़्यादा मारूफ़ हैं। मदीना मुनव्वरा के ‘फ़ुक़हा-ए-सबआ’ में कुछ लोग उनसे प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए।
फ़िक़ही मसलकों का जन्म
इन कारणों के आधार पर विभिन्न इलाक़ों में विभिन्न प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहाद के तरीक़े प्रचलित हुए। जब ताबिईन का ज़माना समाप्त हुआ और तबा-ताबिईन का ज़माना आया तो उस समय तक मुस्लिम जगत् इतना फैल गया था कि इससे ज़्यादा फैलाव मुसलमानों के इतिहास में फिर कभी नहीं आया। कोई एक इस्लामी हुकूमत इतनी बड़ी कभी नहीं हुई जितनी तबा-ताबिईन के ज़माने में हुई। उमवी ख़लीफ़ा अमीरुल-मोमिनीन वलीद-बिन-अब्दुल-मलिक की हुकूमत इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी हुकूमत थी। उनका ज़माना छोटे ताबिईन और बड़े तबा-ताबिईन का ज़माना है, जिसमें फ़ुक़हा-ए-सबआ भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े ताबिईन में से हैं। तबा-ताबिईन भी बड़ी संख्या में मौजूद थे जो ज्ञान और विद्वता के मैदान में सेवा कर रहे थे। उनमें से बहुत-से लोगों ने अपनी किताबें लिखीं और बहुत-से दूसरों ने किताबें तो नहीं लिखीं, लेकिन दर्स (इस्लाम की शिक्षा देने) के ग्रुप क़ायम किए। अब हमारे लिए यह पूछना कि जी अमुक बुज़ुर्ग ने किताबें क्यों नहीं लिखीं और अमुक ने क्यों लिखीं, यह बड़ा अप्रासंगिक सवाल है। उनमें कुछ लोगों ने किताबें लिखीं। कुछ ने नहीं लिखीं। जिन्होंने लिखीं उनमें भी कुछ की किताबें हम तक पहुँचीं। कुछ की किताबें हम तक नहीं पहुँचीं। अल्लाह को मालूम है कि जिनके दिल में उसने किताब लिखने की बात डाली तो क्यों डाली और जिसके दिल में किताब लिखने की बात नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली। यह तो अल्लाह को मालूम है। जिन लोगों की किताबें हम तक पहुँचीं वे क्यों पहुँचीं। और जिन-जिनकी किताबें हम तक नहीं पहुँचीं वे कुछ क्यों नहीं पहुँचीं, ये भी हमें मालूम नहीं। अलबत्ता इतना हमें मालूम है कि कुछ बुज़ुर्गों ने अपनी रायें, इज्तिहादात और तहक़ीक़ात किताबी रूप में संकलित कर लीं। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे कि जिनको बड़ी संख्या में शिष्य भी मिले और कुछ को ज़ाहिर है कि ज़्यादा संख्या में शिष्य नहीं मिले और अगर मिले तो किसी वजह से यह सिलसिला जारी न रह सका। या थोड़े शिष्य मिले। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ क़ाज़ी साहिबान ऐसे नियुक्त हुए कि जो किसी एक ख़ास फ़क़ीह के इज्तिहाद पर फ़ैसला करने को बेहतर समझते थे। कुछ और क़ाज़ी थे जो अपने इज्तिहाद पर फ़ैसले करते थे। जो क़ाज़ी लोग स्वयं अपने इज्तिहाद पर फ़ैसले करते थे वे समय गुज़रने के साथ-साथ संख्या में कम होते गए और उन क़ाज़ियों की संख्या बढ़ने लगी, जो दूसरे फ़ुक़हा के इज्तिहादात पर फ़ैसले करते रहे। अब कुछ प्रतिष्ठित फ़ुक़हा ऐसे थे कि जिनके इज्तिहादात के अनुसार ज़्यादा क़ाज़ियों ने फ़ैसले दिए। कुछ के इज्तिहादात के अनुसार कम क़ाज़ियों ने फ़ैसले दिए। यह सब अल्लाह की तरफ़ से है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। दूसरे क़ाज़ी साहिबान के दिल में क्यों ऐसी बात आई कि एक ख़ास फ़क़ीह के इज्तिहाद के अनुसार फ़ैसले दें और एक-दूसरे फ़क़ीह के इज्तिहादात के अनुसार फ़ैसले न दें। उन्होंने ऐसा ही किया।
कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ फ़ुक़हा ने अपने इज्तिहादात को बड़े rational और logical अंदाज़ में संकलित किया। और एक सुगठित व्यवस्था क़ायम की। कुछ लोगों को ऐसा करने का मौक़ा नहीं मिला। इन सब कारणों एवं कारकों का कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि जिन फ़ुक़हा की रायें किताबी रूप में संकलित हो गईं, जिनके शिष्यों की संख्या ज़्यादा थी, जिनके फ़ैसले और इज्तिहादात पर क़ाज़ियों और मुफ़्तियों ने फ़तवे देने शुरू किए, जिनके फ़िक़ही इज्तिहादात ज़्यादा बौद्धिक और क्रमबद्ध रूप में संकलित हो गए उनके इज्तिहादात एवं शोधों को असाधारण प्रोत्साहन और लोकप्रियता प्राप्त हुई और उनके इज्तिहादात को व्यवहार में लानेवालों और उनके शोधों से सहमति रखनेवालों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। यों थोड़ा ही समय गुज़रा था कि उनके नाम से फ़िक़ही मसलक अस्तित्व में आ गए। उदाहरणार्थ इमाम शाफ़िई (रह॰) ने ‘किताबुल-उम्म’ के नाम से किताब लिखी। यह किताब आठ मोटी जिल्दों में है। इस किताब में स्वयं उन्होंने अपनी हर राय तर्क के साथ संकलित कर दी। ज़ाहिर है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के क़लम से निकली हुई किताब है तो बहुत क़ीमती चीज़ है। शैक्षिक, वैचारिक और क़ानूनी हवाले से इसका जो असाधारण प्रभाव हुआ होगा वह उन फ़ुक़हा का नहीं हुआ होगा जिन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। लोग उनके दर्स में बैठते थे। वे दुनिया से चले गए तो यह सिलसिला भी समाप्त हो गया। उनके विपरीत उदाहरणार्थ इमाम शाफ़िई (रह॰) की किताब मौजूद है तो दर्स का सिलसिला भी यों समझिए कि आज तक जारी और मौजूद है। दुनिया की कोई लाइब्रेरी इस किताब से ख़ाली नहीं है। मिस्र में इमाम शाफ़िई (रह॰) के अपने ज़माने में और उनकी मौजूदगी में उनके सीनियर उस्ताद इमाम लैस-बिन-सअद भी मौजूद थे। इमाम लैस इमाम शाफ़िई (रह॰) के उस्ताद थे। बहुत सम्भव है कि वे इमाम शाफ़िई (रह॰) से बड़े फ़क़ीह, बड़े मुहद्दिस और बड़े उस्ताद हों, लेकिन चूँकि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, इसलिए उनके इज्तिहादात से लाभान्वित होने का सिलसिला उनके जीवन के बाद बहुत कम और सीमित हो गया। उनके शिष्यों की संख्या भी थोड़ी थी। इसलिए उनकी फ़िक़्ह भी उनके बाद कुछ वर्षों तक ही चली और बाद में समाप्त हो गई और आज उनका फ़िक़ही मसलक मौजूद नहीं। इसके विपरीत इमाम शाफ़िई (रह॰) ने अपने इज्तिहादात पर मोटी किताब लिखी। इस किताब को आज तक लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। सर्वोच्च अल्लाह ने उनको ऐसे-ऐसे शिष्य दिए कि जिन्होंने ज़िंदगी-भर उनका दामन नहीं छोड़ा। इन शिष्यों के अपने-अपने प्रभाव भी हुए होंगे। उनके शिष्यों में बहुत बड़े-बड़े और असाधारण व्यक्तित्व शामिल थे, जिनका प्रभाव सामने आए बिना कैसे रह सकता था।
इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) कूफ़ा में बैठकर यह काम कर रहे थे। कूफ़ा में हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और दूसरे कई सहाबा के इज्तिहादात से लोग परिचित चले आ रहे थे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शिष्यों में सबसे अधिक नुमायाँ नाम हज़रत अलक़मा का है। ये प्रसिद्ध ताबिई हैं और दीन की समझ और अन्तर्दृष्टि में इतना ऊँचा स्थान रखते हैं कि एक बार इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने फ़रमाया कि अगर सहाबी होने का सम्मान न होता तो मैं यह कहता कि अलक़मा कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से भी ज़्यादा दीन की समझ रखते हैं। लेकिन चूँकि सहाबी का स्थान बहरहाल ऊँचा होता है इसलिए मैं यह नहीं कहता। उनके शिष्य हज़रत इबराहीम नख़ई ताबिईन में इतने बड़े दर्जे के फ़क़ीह और मुहद्दिस शुमार होते हैं कि उनके इज्तिहादात और कथन हदीस की किताबों में बिखरे हुए हैं। लेखक अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और लेखक इब्ने-अबी-शैबा जिन्होंने ताबिईन के कथन भी जमा करने का प्रबन्ध किया है। इस में इबराहीम नख़ई के इज्तिहादात उस समय सैंकड़ों, बल्कि शायद हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। इबराहीम नख़ई के एक शिष्य हम्माद-बिन-अबी-सुलैमान थे। हम्माद-बिन-अबी-सुलैमान के शिष्य इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) थे जिन्होंने कूफ़ा में लगभग चालीस-पचास वर्ष फ़िक़्ह की शिक्षा दी।
इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) का दर्स आम फ़ुक़हा के अंदाज़ से अलग था। उनका तरीक़ा यह नहीं था कि वे कुछ पढ़ाएँ और लोग नोट करें। वे यकतरफ़ा दर्स नहीं दिया करते थे। उनका तरीक़ा यह था कि वे हर एक को अपने हल्क़ा-ए-दर्स (क्लास) में दाख़िला नहीं देते थे। बड़ी सीमित संख्या में शिष्यों को दाख़िला दिया करते थे। पहले से बड़ा पक्का ज्ञान लेकर आओ, फिर इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के हलक़ा-ए-दर्स में शामिल हो जाओ। किसी नवोदित शिष्य के पास अगर पहले से ज्ञान नहीं होता था तो फिर शिष्य को एक लम्बे समय तक चुपचाप बैठना पड़ता था। और जब ज़रा प्रशिक्षण हो जाता था और इमाम साहब अनुमति दे देते तो फिर कुछ बहस में हिस्सा लेने का मौक़ा मिलता। जिन लोगों को चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति होती थी उनकी संख्या चालीस-पचास और कभी सत्तर-अस्सी तक हो जाती थी। शेष लोग सुननेवाले होते थे। तरीक़ा यह होता था कि इमाम साहब कोई सवाल सामने रख देते थे। हलक़ा-ए-दर्स के भाग लेनेवाले उसका जवाब देते थे और अपने-अपने जवाब के हक़ में क़ुरआन और हदीस से तर्क पेश किया करते थे। फिर इसपर कई-कई दिन तक बहस होती रहती थी और आख़िर में इमाम साहब अपनी नपी-तुली राय देते थे। अधिकांश तो यही होता कि सब लोग इमाम साहब की राय से सहमत हो जाते थे। कभी-कभी कुछ लोग इमाम साहब की बात से मतभेद भी कर लेते थे। काफ़ी बहस के बाद यह भी हुआ कि न इमाम साहब की राय में कोई परिवर्तन आ रहा है और न ही शिष्यों की राय बदल रही है तो दोनों रायें लिख दी जाती थीं। इस तरह से कुछ लोग इन इज्तिहादात और तमाम बहसों को क़लमबंद करते रहते और यों दर्जनों किताबें तैयार हो गईं। यह अंदाज़ व्यक्तिगत रूप से काम करनेवाले फ़ुक़हा के काम से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। एक फ़क़ीह एकान्तवासी होकर लिख रहे हैं और एक-दूसरे फ़क़ीह चालीस पचास बड़े विद्वानों के हलक़े में सामूहिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एक चीज़ संकलित कर रहे हैं। ज़ाहिर है दोनों के स्तर, परिपक्वता और तर्क-शक्ति में ज़मीन-आसमान का अन्तर होगा।
इस तरह इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के इज्तिहादात को उनके शिष्यों ने संकलित कर लिया। उनके शिष्यों में इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी ने सबसे बड़ी संख्या में उनके इज्तिहादात को संकलित किया। उन्होंने दर्जनों किताबें लिखीं। और इस पूरी चालीस या पचास या साठ सदस्यीय कमेटी या अकैडमी के इज्तिहादात उन्होंने क़लमबंद करके संकलित कर डाले। इन सामूहिक इज्तिहादात के अलावा उनकी निजी राय और अपना ज्ञान यह सब इन किताबों में मौजूद हैं। ये किताबें आरम्भ से लोकप्रिय हुईं।
अगर भूगोल आपके सामने हो तो ज़रा नोट करें कि इमाम मुहम्मद ने यह काम बग़दाद और कूफ़ा में बैठकर किया। ये दोनों शहर मुस्लिम जगत् में ऐसे स्थानों पर स्थित थे कि पूरब से जो आएगा उसके लिए सबसे पहले ज्ञानपरक केन्द्र कूफ़ा या बग़दाद होगा। कूफ़ा या बग़दाद के पूरब में स्थित इलाक़े तो बाद में फ़त्ह हुए थे। वहाँ इस्लामी ज्ञान-विज्ञान की वह चर्चा अभी शुरू नहीं हुई थी जो कूफ़ा, बस्रा, बग़दाद और दमिशक़ जैसे पुराने शहरों में थी। ज़ाहिर है इस दौर में उदाहरणार्थ मुल्तान में कोई बड़ा ज्ञानपरक केन्द्र अभी तक नहीं था। देबल, नीशापुर, ग्वादर और ज़ाहिदाँ में ऐसे केन्द्र मौजूद नहीं थे। सबसे क़रीब ज्ञानपरक सभाएँ बग़दाद या कूफ़ा ही में होती थीं। अत: पूर्वी मुस्लिम जगत् के इस पूरे इलाक़े से जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते थे, वह अवश्य प्राचीन ज्ञानपरक केन्द्रों ही में जाते थे। चुनाँचे सबसे पहले वे कूफ़ा और बग़दाद पहुँचते थे। यहाँ इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) और इमाम मुहम्मद के सैंकड़ों शिष्य मौजूद थे। फिर इन शिष्यों के शिष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने-अपने इलाक़ों में फैल जाते थे और उन किताबों की नक़्लें लेकर जाते थे। यों इस पूरे इलाक़े में यानी मध्य एशीया, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान का अधिकतर हिस्से, भारत और बंगला देश में इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के इज्तिहाद की शैली प्रचलित हो गई। इसी तरह उत्तरी अफ़्रीक़ा में ज्ञान का एक बड़ा केन्द्र कैरुआन (Kairouan) बना। कैरुआन ट्यूनीशीया में स्थित है। ताबिईन के ज़माने में यह पूरा इलाक़ा फ़त्ह हो चुका था। स्पेन की सीमा तक मुसलमान पहुँच चुके थे। यह वह ज़माना था कि जब इस पूरे इलाक़े की बहुसंख्या ग़ैर-मुस्लिम थी। और उन ग़ैर-मुस्लिमों में ऐसे लोग भी थे जो समय-समय पर मुसलमानों पर हमले करते रहते थे। कोई शहर भी ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमानों की बहुलता हो। अगरचे इन मुसलमानों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन थे वे अल्पसंख्या ही में, अभी तक मदीना और कूफ़ा या बस्रा की तरह कोई भी शहर सौ प्रतिशत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूरे उत्तरी अफ़्रीक़ा में नहीं था। मुसलमानों ने यह चाहा कि जिस तरह कूफ़ा और बस्रा सौ प्रतिशत मुस्लिम आबादियाँ हैं, उसी तरह का एक शहर यहाँ उत्तरी अफ़्रीक़ा में भी बसाया जाए। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन ने जब इस ग़रज़ के लिए पूरे इलाक़े का जायज़ा लिया तो भौगोलिक रूप से एक ऐसा उचित और सुरक्षित क्षेत्र नज़र आया जो मुसलमानों की बस्ती या छावनी बनाने के लिए बहुत उचित नज़र आता था। लेकिन यह क्षेत्र जंगलों से भरा था। पहाड़ों के आँचल में था, इसलिए सैन्य दृष्टि से सुरक्षित था। संसाधन उपलब्ध थे। पानी प्रचुर मात्रा में था। इलाक़ा हरा-भरा था। यह कैरुआन शहर इस इलाक़े में पहला इस्लामी शहर था जिसमें सौ प्रतिशत मुस्लिम आबादी थी। यही कैरुआन इस इलाक़े का एक महत्वपूर्ण ज्ञानपरक केन्द्र क़रार पाया।
इमाम मालिक (रह॰) के अधिकतर शिष्य मुस्लिम जगत् के पश्चिमी इलाक़े से आए थे और इस इलाक़े से आनेवालों के रास्ते में बड़ा केन्द्र मदीना मुनव्वरा पड़ता था। इमाम मालिक (रह॰) के कुछ शिष्य कैरुआन में जाकर बसे। उनके एक शिष्य थे क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात। वे लम्बे समय इमाम मालिक (रह॰) के पास रहे थे और उनके इज्तिहादात एक किताबी शक्ल में संकलित कर चुके थे। यह इज्तिहादात मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) के अलावा थे। ये सारे इज्तिहादात और अपने नोट्स और याददाश्तें लेकर वह कैरुआन चले गए। वहाँ उन्होंने अपना हल्क़ा (ग्रुप) बनाया। अब आसपास के इलाक़ों में जो व्यक्ति भी इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करना चाहता तो वह कैरुआन जाता था और असद-बिन-फ़ुरात और उनके शिष्यों से ज्ञान प्राप्त करता था। वहाँ उन्होंने इमाम मालिक (रह॰) के तमाम इज्तिहादात को संकलित किया और ‘असदिया’ के नाम से एक किताब लिखी। किताब का नाम ‘असदिया’ इसलिए पड़ गया कि यह असद-बिन-फ़ुरात ने संकलित की थी, लेकिन इज्तिहादात इसमें सारे के सारे इमाम मालिक (रह॰) ही के हैं।
ये किताब जो अनेक भागों में थी, पूरे इलाक़े में बहुत लोकप्रिय हुई और इसकी वजह से आसपास में इमाम मालिक (रह॰) के इज्तिहादात प्रचलित हो गए। जो लोग पढ़ने आते थे वे इमाम मालिक (रह॰) के शिष्यों से ज्ञान प्राप्त करते थे। मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) भी पढ़ते थे और उसके और ‘असदिया’ के नुस्ख़े भी साथ ले जाते थे। चूँकि शिष्य भी इमाम मालिक (रह॰) के थे और किताबें भी उन ही की थीं। अत: उन सब इलाक़ों में फ़िक़्हे-मालिकी प्रचलित हो गई।
क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात इस इलाक़े के क़ाज़ी भी हो गए। उन्होंने फ़िक़्हे-मालिकी के अनुसार फ़ैसले करने शुरू कर दिए। आम लोगों को जब पता चला कि फ़ैसले फ़िक़्हे-मालिकी के अनुसार हो रहे हैं तो उन्होंने फ़िक़्हे-मालिकी को पढ़ने और सीखने पर ध्यान दिया। क़ाज़ी असद के कुछ समय बाद इमाम मालिक (रह॰) के एक और शिष्य, जो उनके प्रत्यक्ष रूप से शिष्य तो नहीं थे, लेकिन उनके बहुत-से शिष्यों के शिष्य थे, इमाम सहनून-बिन-सईद उस इलाक़े के सबसे बड़े ज्ञानपरक व्यक्तित्व बनकर उभरे। ये फ़िक़्हे-मालिकी में बहुत ऊँचा दर्जा रखते हैं। वे कैरुआन में असद-बिन-फ़ुरात की जगह बैठे। ‘असदिया’ किताब का दर्स देते रहे। इस दौरान उन्होंने ‘असदिया’ का एक नया एडिशन तैयार कर लिया। इसमें क्रम की दृष्टि से और बेहतरी पैदा की। और अधिक जानकारियाँ शामिल कीं और सात मोटी जिल्दों में एक किताब लिखी जो ‘अल-मुदव्वनतुल-कुबरा’ कहलाती है। यह किताब वस्तुतः इमाम मालिक (रह॰) की किताब है, लेकिन सहनून-बिन-सईद ने इसको संकलित किया। ‘अल-मुदव्वनतुल-कुबरा’ उस दिन से लेकर आज तक मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) के साथ-साथ फ़िक़्हे-मालिकी का सबसे बड़ा स्रोत है। मात्रा दृष्टि से ‘अल-मुदव्वनतुल-कुबरा’ और गुणवत्ता की दृष्टि से मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) को फ़िक़्हे-मालिकी में मौलिक और मूल हैसियत प्राप्त है। इस तरह यह पूरा इलाक़ा यानी पूरा, ट्यूनीशीया, लीबिया, मराक़श, अल-जज़ाइर वग़ैरा फ़िक़्हे-मालिकी का केन्द्र बन गए। और फिर जब इस इलाक़े से इस्लाम के प्रचारकों के क़ाफ़िले दक्षिण की ओर यानी काले अफ़्रीक़ा की तरफ़ बढ़ने शुरू हुए तो वहाँ भी जो लोग इस्लाम स्वीकार करते गए, फ़िक़्हे-मालिकी को अपनाते गए। इसलिए पूरा पश्चिमी अफ़्रीक़ा, पूरा मोरीतानिया, नाईजीरिया, नाइजर और सेनेगल सहित यह सारा इलाक़ा मालिकी है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से फ़िक़्हे-मालिकी प्रचलित हो गई। इसी तरह के कारण शेष फ़िक़ही मसलकों के विभिन्न इलाक़ों में प्रचलित होने के बारे में हैं।
तमाम फ़िक़ही मसलक जो अस्तित्व में आए उनकी सही संख्या तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन अनुमानित रूप से यह संख्या सैंकड़ों में थी। इसलिए कि सैंकड़ों बड़े-बड़े फ़ुक़हा थे जो यह काम कर रहे थे। उनमें से जिन-जिनको यह साधन और सुविधाएँ उपलब्ध आ गईं, उनकी फ़िक़्हें शेष रहीं और जिनको ये साधन और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं आईं उनकी फ़िक़्हें समाप्त हो गईं। जो फ़िक़्हें बाक़ी रहीं उनकी संख्या भी पंद्रह-बीस के क़रीब थी। लेकिन उनमें कुछ समय गुज़रने के साथ-साथ समाप्त हो गईं। उदाहरणार्थ इमाम अबदुर्रहमान-बिन-अबी-लैला इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के समकालीन थे। उनकी अलग फ़िक़्ह थी। इमाम अब्दुर्रहमान अल-औज़ाई भी इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के समकालीन थे। उनकी भी अलग फ़िक़्ह थी। इमाम सुफ़ियान सौरी जो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के ज़रा जूनियर समकालीन थे। उनकी अपनी फ़िक़्ह थी। इब्ने-जरीर तबरी की अपनी फ़िक़्ह थी। इमाम दाऊद-बिन-सुलैमान अज़-ज़ाहिरी की अलग फ़िक़्ह थी। ये सारी फ़िक़्हें एक-एक करके विभिन्न कारणों से समाप्त हो गईं। उनमें से कोई फ़िक़्ह अपने संस्थापक के देहान्त पर समाप्त हो गई। कोई उनके बाद एक या दो नस्लों तक क़ायम रही। कोई दो सौ वर्ष चली, कोई तीन सौ वर्ष चली। कुछ के साथ यह भी हुआ कि किसी दूसरी क़रीबी और समान फ़िक़्ह में विलीन हो गई। उदाहरणार्थ इमाम इब्ने-जरीर तबरी और इमाम शाफ़िई (रह॰) के विचारों में ज़्यादा अन्तर नहीं था। फ़िक़्हे-शाफ़िई (रह॰) और फ़िक़्हे-तबरी में आम तौर से आंशिक अन्तर था जो समय के साथ समाप्त हो गया और सारे तबरी शाफ़िई हो गए। इमाम औज़ाई के विचार अक्सर एवं अधिकतर इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के विचारों से मिलते-जुलते थे। उनके माननेवाले इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के माननेवालों में शामिल हो गए। इस तरह से होते-होते जो फ़िक़्हें शेष रह गईं वे ये आठ हैं—
1. फ़िक़्हे-हनफ़ी
2. फ़िक़्हे-मालिकी
3. फ़िक़्हे-शाफ़िई
4. फ़िक़्हे-हंबली
5. फ़िक़्हे-जाफ़री
6. फ़िक़्हे-इबाज़ी
7. फ़िक़्हे-ज़ैदी
8. फ़िक़्हे-ज़ाहिरी
इनमें संख्या की दृष्टि से सबसे पहले फ़िक़्हे-हनफ़ी का दर्जा है। फिर फ़िक़्ह शाफ़िई (रह॰) का दर्जा है फिर फ़िक़्हे-मालिकी है। फिर सुन्नियों में सबसे छोटी फ़िक़्ह, फ़िक़्हे-हंबली है। अहले-सुन्नत (सुन्नियों) के अलावा जो चार फ़ुक़हा हैं उनमें सबसे बड़ी फ़िक़्ह, फ़िक़्ह जाफ़री है। अस्ना-अशरी शीया जिसको मानते हैं। फिर फ़िक़्हे-ज़ैदी है जिसपर यमन के शीया अमल करते हैं। यह फ़िक़्ह इमाम ज़ैद-बिन-अली-बिन-हुसैन-बिन-अली-बिन-अबी तालिब से जोड़ी जाती है। उनकी किताब ‘किताबुल-मजमूअ’ हदीस और फ़िक़्ह की सबसे पहली किताब है जो हम तक पहुँची है। फ़िक़्हे-ज़ाहिरी भी किसी-न-किसी शक्ल में विभिन्न नामों से मौजूद है और लोग उसपर अमल कर रहे हैं। इसके प्रभाव भी हो रहे हैं। फ़िक़्हे-ज़ाहिरी के संस्थापक की अपनी तो कोई किताब आज उपलब्ध नहीं। अलबत्ता उनके विचारों और इज्तिहादात का उल्लेख किताबों में बहुत अधिक मिलता है। उनके माननेवालों में इमाम अबू-बक्र अली इब्ने-हज़म के रूप में एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व पैदा हुआ जो शायद मानव इतिहास के कुछ विशिष्ठ व्यक्तित्व में से एक हैं। उनकी मृत्यु 457 हिजरी में हुई। उनकी दो किताबें हैं, जिनमें ‘अल-अहकाम फ़ी उसूलिल-अहकाम’ उसूले-फ़िक़्ह पर है और ‘अल-मुहल्ला’, बहुत-सी जिल्दों में एक फ़िक़ही इंसाइक्लोपेडिया है। असाधारण गहराई के साथ उन्होंने फ़िक़ही मामलों पर ग़ौर किया। ज़ाहिरी फ़ुक़हा ‘क़ियास’ (अनुमान) के क़ाइल नहीं थे और इसको शरीअत का स्रोत नहीं समझते थे। इसलिए जहाँ शेष फ़ुक़हा ने ‘क़ियास’ से काम लिया, वे ‘क़ियास’ से काम नहीं लेते थे। ज़ाहिर है कि इससे बहुत-से इज्तिहादात और फ़िक़ही रायों में अन्तर पैदा होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता न हो वहाँ वह पवित्र क़ुरआन और हदीसों में सांकेतिकता के अस्तित्व को भी नहीं मानते। कोशिश करते हैं कि शब्द की व्याख्या शब्दकोशीय अर्थों की दृष्टि से करें। इससे कुछ जगह व्याख्या में मतभेद पैदा होता है।
ये वे कारण हैं जिनके आधार पर विभिन्न इलाक़ों में विभिन्न फ़िक़ही मसलक और मज़हब प्रचलित हुए। इसमें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दौर से लेकर इमामों के मसलक तक इन व्यक्तियों के अपने निजी प्रशिक्षण, निजी प्रवृत्ति, स्वभाव, क्षेत्र और परिस्थितियों की विविधता, हर दृष्टि से अन्तर पैदा हुआ है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक फ़क़ीह ने एक इलाक़े में बैठकर जो इज्तिहादात संकलित किए, वे एक विशेष ढंग के थे, लेकिन जब वही फ़क़ीह दूसरे इलाक़े में गए तो वहाँ की परिस्थितियों पर ग़ौर करने से उनके विचारों में परिवर्तन आया, जिसके परिणामस्वरूप उनके इज्तिहादात भी बदल गए। इस मामले में सबसे नुमायाँ उदाहरण इमाम शाफ़िई (रह॰) का है। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यमन और मक्का मुकर्रमा में गुज़रा था। यमन और मक्का मुकर्रमा में परिस्थितियाँ तुलनात्मक रूप से ज़रा बिगड़ी हुई थीं। सादगी नुमायाँ थी। इसलिए उन्होंने जो फ़िक़्ह यहाँ बैठकर संकलित की उसमें कुछ आदेश दिए गए। इन आदेशों को उन्होंने ‘किताबुल-हुज्जः’ के नाम से एक किताब के रूप में संकलित किया। बाद में इमाम शाफ़िई (रह॰) बग़दाद आए। बग़दाद अब्बासी साम्राज्य की राजधानी था और उसमें दिन-प्रतिदिन विकास हो रहा था। नए-नए शहर बस रहे थे और लोग दुनिया-भर से वहाँ आ रहे थे। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने जब बग़दाद की परिस्थितियों को देखा तो अपने विचारों में कई चीज़ों को परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की। बग़दाद के बाद क़ाहिरा गए तो वह भी अफ़्रीक़ा का सबसे बड़ा शहर था। फ़ुसतात (Fustat) के क़रीब आबाद था जो मुसलमानों का सबसे बड़ा सैन्य केन्द्र और अफ़्रीक़ा का सबसे पहला मुसलमान आबादीवाला शहर था। तो यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर उन्होंने नए सिरे से एक नई फ़िक़्ह संकलित की। और ‘किताबुल-उम्म’ के नाम से एक नई किताब तैयार की, जो आज मौजूद है। ‘किताबुल-हुज्जः’ आज मौजूद नहीं है। मैं लम्बे समय से इसकी तलाश में हूँ। मेरी इच्छाओं की फ़ेहरिस्त में एक यह भी है कि कहीं से ‘किताबुल-हुज्जः’ उपलब्ध हो सके। ‘किताबुल-हुज्जः’ और ‘किताबुल-उम्म’ में तुलना की जाए और देखा जाए कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के विचारों में कहाँ-कहाँ परिवर्तन आया। इस तुलनात्मक अध्ययन से पता चलेगा कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के इज्तिहादात में परिस्थितियों और घटनाओं के अन्तर से क्या-क्या परिवर्तन आए और किन परिस्थितियों और कारणों से आए। ‘किताबुल-हुज्जः’ की बातें विभिन्न किताबों में बिखरी हुई तो मिल जाती हैं, कहीं इकट्ठा नहीं मिलतीं। इमाम शाफ़िई (रह॰) के बारे में फ़िक़्ह की अधिकांश किताबों में लिखा हुआ देखा गया है कि “इमाम शाफ़िई (रह॰) प्राचीन कथन में यह कहते हैं और वर्तमान कथन में यह कहते हैं। अक्सर मामलों में उनके दो कथन हैं। यानी प्राचीन कथन जो ‘किताबुल-हुज्जः’ में लिखा हुआ था, और वर्तमान कथन जो ‘किताबुल-जदीद’ में दर्ज है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। यह इस पूरे इतिहास का अत्यन्त संक्षिप्त सार है जो फ़िक़्हे-इस्लामी के गठन के दौर को बयान करता है। यह वह दौर है जब अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन ने असाधारण इज्तिहादी अन्तर्दृष्टि के नमूने दुनिया को दिखाये और अपने-अपने फ़िक़ही मसलक संकलित किए।
सवालात
सवाल : स्वभाव की विविधता के हवाले से आज की चर्चा ने ज़ेहन को बहुत स्पष्ट किया है लेकिन एक सवाल उभरता है कि जब स्वभाव की विविधता इतनी प्रभावशाली होती है तो क्या इससे इज्तिहादात की हैसियत कम या ज़्यादा न होगी?
जवाब : इज्तिहाद की हैसियत केवल क़ुरआन और सुन्नत के पैमाने की वजह से कम या ज़्यादा होगी। अगर किसी की निजी दिलचस्पी क़ुरआन और सुन्नत के पैमाने में स्वीकार्य है तो वह इज्तिहाद स्वीकार्य है। अगर इस पैमाने में वह हल्का है तो अस्वीकार्य है। केवल किसी की निजी दिलचस्पी की वजह से इसको स्वीकार्य या अस्वीकार्य नहीं समझा जाएगा। उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है कि सर्वोच्च अल्लाह ने समुद्र से ‘लहमन तरीयन’ तुम्हारे लिए निकाला है। और एक जगह आया है कि أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ कि तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना जायज़ क़रार दिया जाता है। مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ, तुम्हारे लिए भी और क़ाफ़िलों के लिए भी। ये दो आयतें हैं जिनमें एक जगह ‘लहमे-तरीयन’ यानी तरोताज़ा गोश्त का ज़िक्र है और दूसरी जगह शिकार का और एक जगह खाने का आदेश है। अब आप रुचि को देखें कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) कूफ़ा में बैठे हैं। जहाँ एक तरफ़ दजला बहता है और दूसरी तरफ़ फ़ुरात बहता है और वहाँ जो चीज़ सबसे सस्ती मिलती होगी वह शायद मछली हो। इतनी ज़्यादा मछली मिलती होगी कि जिसका कोई शुमार नहीं। इमाम मालिक (रह॰) मदीना मुनव्वरा में बैठे होते थे जहाँ मछली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सबसे क़रीब जगह जहाँ से मछली मिल सकती थी वह राबिग़ की बंदरगाह है जहाँ उस ज़माने में आदमी कम-से-कम दस दिन में मदीना पहुँचता होगा। अब मछली दस दिन तो क्या एक दो दिन में ख़राब हो जाती है। तो गोया मदीना मुनव्वरा में मछली बहुत मुश्किल थी। अब इमाम मालिक (रह॰) ने सैद, तआम और लहमे-तरी तीनों के अलग-अलग अर्थ लिए। इमाम मालिक (रह॰) ने कहा कि लह्मे-तरी से मुराद वह गोश्त है जो आदमी समुद्र से ताज़ा-ब-ताज़ा ले-ले। लेकिन सैद और तआम दो अलग-अलग अर्थों में आया है। तआम से मुराद हर वह समुद्री चीज़ है जो वहाँ पैदा हो रही हो तो उसको प्रयुक्त किया जा सकता है। अत: समुद्र में पैदा होनेवाला केकड़ा, कछुआ और तमाम समुद्री जानवर हलाल हैं। इन सबको ‘लह्मे-तरीया’ के आम अर्थों में लिया जाएगा। शब्दकोश की दृष्टि से इसकी गुंजाइश मौजूद है। सैद का शब्द भी है और तआम का शब्द भी है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) कूफ़ा में बैठते थे जहाँ मछली बहुत मिलती थी। उन्होंने फ़रमाया कि आम तौर पर समुद्र की जो चीज़ खाई जाती है वह मछली है। पवित्र क़ुरआन में बहुत-से आदेश उर्फ़ के आधार पर दिए गए हैं अत: जो चीज़ उर्फ़ में शामिल नहीं है, वह पवित्र क़ुरआन के अर्थ में शामिल नहीं है। यह एक लंबी बहस है। तो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने फ़रमाया कि केवल मछली जायज़ है और इसके अलावा कोई और समुद्री जानवर जायज़ नहीं है। इमाम मालिक (रह॰) ने फ़रमाया कि हर समुद्री जानवर जायज़ है। अब इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इमाम मालिक (रह॰) की रुचि क्या थी और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की दिलचस्पी क्या थी। आप केवल यह देखेंगे कि क़ुरआन और सुन्नत के शब्द में दोनों रायों की गुंजाइश है कि नहीं है। अगर गुंजाइश है तो ठीक है और अगर पवित्र क़ुरआन के शब्द और अरबी भाषा की दृष्टि से यह गुंजाइश नहीं है तो फिर यह राय स्वीकार्य नहीं है।
सवाल : इज्तिहादात के सिलसिले में आपने ग़ुस्ल (स्नान) की स्थिति में जिस तरह ‘तयम्मुम’ करके दिखाया तो हमने तो किसी हदीस में ऐसा नहीं देखा, हमने तो हदीस में यही पढ़ा है कि ग़ुस्ल की स्थिति में भी नमाज़वाला ‘तयम्मुम’ ही किया जाए।
जवाब : आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आपने हदीस में जो सुना है वही सही है। हदीस के अनुसार ग़ुस्ल की आवश्यकता हो और पानी मौजूद न हो, तो नमाज़ के लिए वुज़ूवाला तयम्मुम ही करो। यानी मिट्टी या पत्थर पर हाथ मॉरो। पहले हाथों पर फेरो फिर दूसरा हाथ मारकर उसको थोड़ा झटको, उसके बाद मुँह पर फेर लो। हदीस में तो यही है और होता भी यही है। लेकिन जब तक यह आदेश स्पष्ट नहीं हुआ था उस समय एक सहाबी को इसकी आवश्यकता पेश आई। उनको मालूम नहीं था कि नबी (सल्ल०) ने यह जो तयम्मुम का आदेश दिया है यह केवल वुज़ू के लिए है या ग़ुस्ल के लिए भी यही आदेश है। उन्होंने अपने दिमाग़ से यह समझा कि शायद मिट्टी में लोट-पोट होना ग़ुस्ल के लिए ज़रूरी हो। उन्होंने ऐसा ही किया। आकर नबी (सल्ल०) को सूचना दी। उन्होंने फ़रमाया कि यह ज़रूरी नहीं था। यह सारी घटना भी हदीस ही की किताबों में लिखी हुई है। मैंने भी हदीस की किताब से लिया है। मुझे हज़रत अम्मार ने सीधे आकर नहीं बताया था। हदीस की किताब ही में यह लिखा हुआ है।
सवाल : The emergence of various schools has been very nicely elaborated by you, Jazak Allah. However, it is not yet clear as to not yet how certain things which are Halal or permissible for us but are Haram for Shiah groups, such as opening fast with the first Azan after Maghrib but Shiahs delayed it.
[विभिन्न मसलकों के पैदा होने को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, जज़ाक अल्लाह। मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए हलाल या जायज़ हैं, लेकिन शीया समूहों के लिए हराम हैं, जैसे कि मग़रिब के बाद पहली अज़ान के साथ रोज़ा खोलना लेकिन शीया इसे देर से करते हैं।]
जवाब : इस तरह के आंशिक मतभेद ‘नस्स’ की व्याख्या में अन्तर की वजह से पैदा हो जाते हैं। इसी रोज़े का उदाहरण लीजिए। पवित्र क़ुरआन में आया है कि ‘अतिम्मुस्सिया-म इलल-लैल’ कि रोज़े को पूरा करो रात तक। अब यहाँ दो शब्द आए हैं ‘लैल’ और ‘इला’। यानी रात और तक। इसपर बहुत लम्बी और विस्तृत बहस हुई है जिसके उल्लेख के लिए समय नहीं है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने इसका यह अर्थ समझा और फ़ुक़हा की बड़ी संख्या ने यही अर्थ लिया कि जब तक ‘लैल’ दाख़िल न हो जाए उस समय तक रोज़ा रखा जाए। जब ‘लैल’ का दाख़िल होना शुरू हो जाए तो समझा जाएगा कि ‘नहार’ (दिन) समाप्त हो गया है। उस समय रोज़ा खोल दिया जाएगा। लेकिन ‘लैल’ क्या होती है और यह कब शुरू होती है, फ़ुक़हा की अधिक संख्या का यह कहना है कि जब सूरज की टिकिया नज़रों से ओझल हो जाए और डूब जाए तो रात यानी लैल शुरू हो जाती है। सूरज के लिए टिकिया का शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि अगर आप रेगिस्तान या मैदानी इलाक़े में खड़े हो जाएँ तो अस्त होता हुआ सूरज एक गेंद की तरह नज़र आता है। जैसे फ़ुटबाल होती है। इस गेंद को फ़ुक़हा टिकिया के शब्द से याद करते हैं। तो फ़ुक़हा कहते हैं कि जब सूरज की टिकिया डूबते-डूबते उसका आख़िरी हिस्सा भी डूब जाए तो उस समय समझा जाएगा कि दिन समाप्त हो गया और रात शुरू हो गई। इस समय रोज़ा खोल लिया जाएगा। कुछ फ़ुक़हा जिनमें शीया फ़ुक़हा भी शामिल हैं, वे यह कहते हैं कि मात्र टिकिया का डूबना काफ़ी नहीं है। इसलिए कि टिकिया की रौशनी का डूबना भी ज़रूरी है। एक पीला-पन जिसको शफ़क़ (उषा) कहते हैं वह सूरज की टिकिया डूबने के बाद भी शेष रहता है। जो ख़ासा सुर्ख़ होता है और पहली नज़र में यह निर्धारण करना मुश्किल होता है कि टिकिया डूबी कि नहीं। तो जब तक उसकी सुर्ख़ी ग़ायब नहीं होती, उस समय गोया यह समझा जाए कि टिकिया पूरी तरह से नहीं डूबी। वह शफ़क़ टिकिया के अधीन है। वे यह कहते हैं कि जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अधीन होती है तो अधीन का भी वही आदेश होता है जो अस्ल का होता है। अत: अस्ल और अधीन जब दोनों डूब जाएँ, तब रात शुरू होगी। इस अमल में दस बारह मिनट अधिक समय लगता है। इसलिए वह बारह मिनट और प्रतीक्षा करते हैं। यह मात्र लैल की व्याख्या में मतभेद है। कोई क़ुरआन या सुन्नत में मतभेद नहीं। केवल यह मतभेद है कि लैल किसको कहते हैं। बहुसंख्या के ख़याल में सूरज की टिकिया के ग़ायब होने से रात शुरू हो जाती है। दूसरा पक्ष कहता है कि जब टिकिया के प्रभाव भी डूब जाएँगे तो तब लैल शुरू होगी। मेरा निजी ख़याल यह है कि फ़ुक़हा की अधिकांश बहुसंख्या का कहना दुरुस्त है। इसलिए कि दिन उस समय शुरू होता है जब सूरज निकलने लगता है। सूरज की टिकिया के प्रकट होने से पहले जब उसकी लालिमा या शफ़क़ (उषा) ज़ाहिर होती है उसको दिन का आरम्भ क़रार नहीं दिया जाता। इससे पहले के समय को नहार कहते हैं और इस समय तक फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। यही उसूल टिकिया के ग़ायब होने के समय भी सामने रखना चाहिए। बहरहाल यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसपर किसी भी चर्चा की आवश्यकता हो। ये दो विभिन्न रायें हैं।
Recent posts
-

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -

इल्मे-फ़िक़्ह के विभिन्न विषय (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 4)
25 February 2025