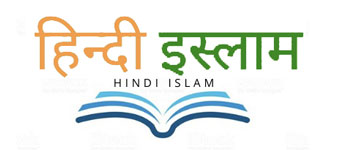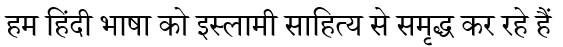शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
-
फ़िक़्ह
- at 16 March 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
आज की चर्चा का शीर्षक है ‘शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद’। शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद, बज़ाहिर ये दोनों अलग-अलग लेख हैं। लेकिन उनमें एक बड़ी गहरी सार्थक अनुकूलता पाई जाती है। शरीअत के उद्देश्य से मुराद वे मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य हैं जो इस्लामी शरीअत के सभी आदेशों में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सामने रहते हैं। एक दृष्टि से इस्लामी शरीअत की आम तत्वदर्शिता के लिए ‘मक़ासिदे-शरीआ’ (शरीअत के उद्देश्य) की शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। शरीअत के आदेशों में जो निहितार्थ छिपे हैं और जो तत्वदर्शिता सामने है, उसका अध्ययन शरीअत के उद्देश्यों के शीर्षक के तहत किया जाता है। शरीअत के उद्देश्यों पर चिन्तन-मनन और इसके विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का आरम्भ उसी दिन से हो गया था जिस दिन इस्लाम के आदेश अवतरित होने शुरू हुए। स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुत-से आदेशों की तत्वदर्शिताएँ बयान कीं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने इन तत्वदर्शिताओं पर ग़ौर किया और बहुत-से बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के कथनों और फ़तवों में इन तत्वदर्शिताओं के बारे में क़ीमती इशारे मिलते हैं। शरीअत जो इंसान की सफलता और कामयाबी का स्पष्ट, खुला, आसान और दो-टूक रास्ता है, जो इंसान को उसके गंतव्य स्थान तक सफलता के साथ पहुँचा देता है। जो इंसान को वास्तविक जीवन के मूलस्रोत तक ले जाने का एक मात्र ज़ामिन है। उसके आदेशों में क्या तत्वदर्शिताएँ और क्या निहितार्थ छिपे हैं, अल्लाह ने ये आदेश क्यों दिए हैं, इसपर मुसलमान आरम्भ से चिन्तन-मनन कर रहे हैं।
शरीअत के उद्देश्यों का अध्ययन क्यों?
आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए। वह यह कि जब हम शरीअत के उद्देश्यों की बात करते हैं या शरीअत की तत्वदर्शिता का सवाल हमारे सामने आता है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम शरीअत के आदेशों पर केवल इसलिए ईमान रखते हैं कि वे अल्लाह की शरीअत के आदेश हैं। हमें शरीअत के आदेश केवल इसलिए मानने चाहिएँ कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इन आदेशों को मानने का आदेश दिया है। अगर अल्लाह और रसूल के सामने शरीअत के आदेशों की कोई तत्वदर्शिता न भी होती तो भी हम इन आदेशों के मानने के इसी तरह पाबंद होते, जैसे अब पाबंद हैं, जब तत्वदर्शिताओं के दफ़्तर के दफ़्तर तैयार हो चुके हैं। इन तत्वदर्शिताओं को जानना या न जानना ईमान और शरीअत पर अमल करने की शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर हम तत्वदर्शिता न जानते हों तब भी ईमान लाना हमारी ज़िम्मेदारी है और शरीअत के आदेशों को मानना और उनपर अमल करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम तत्वदर्शिता जानते भी हों तो इससे हमारे सामने ईमान को बढ़ाना और उसमें परिपक्वता तथा शरीअत के आदेशों पर सन्तुष्टि से कार्यान्वयन ही का उद्देश्य होना चाहिए। तत्वदर्शिता की पहचान और ‘मस्लहत’ की खोज ईमान की पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए। यह बात कि अगर शरीअत की कोई तत्वदर्शिता मेरी समझ में आ गई और मेरी बुद्धि ने शरीअत की तत्वदर्शिता को स्वीकार कर लिया तो मैं शरीअत को मानता हूँ। और अगर मेरी बुद्धि ने शरीअत की तत्वदर्शिता को स्वीकार न किया तो में इसको नहीं मानता, एक ईमानवाले का रवैया नहीं हो सकता। समझ लीजिए कि यह रवैया वास्तव में शरीअत पर ईमान का नहीं है, बल्कि यह अपनी बुद्धि पर ईमान का द्योतक है।
अपनी बुद्धि से तो इंसान हर चीज़ का फ़ैसला करता ही है। कोई दुश्मन भी आपको कोई मेडिकल नुस्ख़ा बताए और आपकी बुद्धि उसको दुरुस्त स्वीकार करे तो आप उसको मान लेते हैं। आपका कोई विरोधी भी अगर आपको किसी समस्या का समाधान बताए और वह आपकी बुद्धि में आ जाए तो आपको उसे मानने में संकोच नहीं होता। इसलिए अगर शरीअत के आदेशों के मानने या न मानने का दारोमदार इंसान की अपनी बुद्धि पर ठहरा दिया जाए तो फिर शरीअत शरीअत नहीं रहती। वह दुनिया के किसी भी आम इंसान के मश्वरे से ज़्यादा महत्व नहीं रखेगी। इसलिए यह बात पहले दिन से साफ़ होनी चाहिए कि एक मुसलमान का काम यह है कि अगर यह साबित हो जाए कि यह आदेश शरीअत का आदेश है, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अमुक बात का आदेश दिया है, तो वह बात हमारे लिए अन्तिम निर्णय होनी चाहिए और इसपर हमारा ईमान इतना मज़बूत होना चाहिए जिस तरह कि इस समय सूरज के पूरी रौशनी के साथ चमकने पर हमारा ईमान है। अगर तत्वदर्शिता समझ में आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे हमारे ईमान में परिपक्वता आ जानी चाहिए। और अगर तत्वदर्शिता समझ में न आए तो इसको अपनी बुद्धि की कमी और अपनी समझ का क़ुसूर समझना चाहिए। यह बात पवित्र क़ुरआन ने भी स्पष्ट कर दी है। सूरा-4 निसा में अल्लाह का कथन है—
“तो तुम्हें अपने रब की क़सम! ये ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में तुमसे फ़ैसला न कराएँ। फिर जो फ़ैसला तुम कर दो, उसपर ये अपने दिल में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह मान लें।” (क़ुरआन, 4:65)
इंसान दिल में तंगी और हरज कब और क्यों महसूस करता है? हरज और तंगी वहीं महसूस होती है जहाँ फ़ैसला अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ महसूस होता है। अल्लाह और रसूल का फ़ैसला सुनने के बावजूद अगर दिल में तंगी महसूस होती है तो इसकी वजह यह है कि बुद्धि में वह बात नहीं आती। आदेश की तत्वदर्शिता और ‘मस्लहत’ (निहितार्थ) उसकी समय समझ में नहीं आती तो इंसान तंगी महसूस करता है।
लेकिन इसके बावजूद शरीअत के आदेशों के निहितार्थों को जानने की कोशिश करना या अल्लाह के कथनों और आदेशों की हिकमतें जानने की इच्छा होना अल्लाह के निकटवर्ती और सदाचारी इंसानों का तरीक़ा रहा है। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने सर्वोच्च अल्लाह से दुआ की कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे ज़िन्दा करते हैं। कहा गया कि “क्या तुम ईमान नहीं रखते?” तो जवाब में हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने बताया कि क्यों नहीं, निस्सन्देह ईमान तो रखता हूँ, लेकिन यह सवाल इसलिए किया है कि मेरे दिल को और अधिक सन्तुष्टि प्राप्त हो जाए। इंसान का स्वभाव यह है कि बहुत-सी निश्चित और क़तई चीज़ों पर वह पक्का विश्वास रखता है, लेकिन और अधिक सन्तुष्टि हो जाती है जब उनको इंसान अपनी आँखों से स्वयं देख लेता है। कभी-कभी आदमी सुनकर ईमान तो ले आता है, बात को मान तो लेता है, लेकिन जिसको परिपक्वता और दिल के सन्तोष की कैफ़ियत कहते हैं वह देखकर ही प्राप्त होती है।
हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) जब हज़रत ख़ज़िर से अलग होने लगे, तो हज़रत खज़िर ने कहा कि आइए मैं आपको यह भी बतादूँ कि यह सब काम मैंने क्यों किए। और फिर उन्होंने एक-एक करके उन सब कामों की तत्वदर्शिता बताई और कहा कि “मैंने उनमें से कोई एक कार्य भी अपने फ़ैसले से नहीं किया था। सब अल्लाह के आदेश से किया था और ये हिकमतें उसके पीछे थीं।” गोया बावजूद इसके कि हज़रत ख़ज़िर को मालूम था कि यह अल्लाह के पैग़ंबर हैं, अल्लाह ही के आदेश से मेरे पास आए हैं और जानते हैं कि मैंने जो किया है अल्लाह के आदेश से किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने यह उचित समझा कि उन कामों की हिकमतें हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को बता दें, ताकि उनका सन्तोष और बढ़ जाए। इन दो उदाहरणों से यह पता चलता है कि शरीअत के आदेशों की हिकमतें जानने की इच्छा रखना और उसकी आवश्यकता महसूस करना एक स्वाभाविक बात है। और अगर किसी ईमानवाले को ये हिकमतें मालूम हों तो वह ज़्यादा इत्मीनान और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ उस बात पर स्वयं भी अमल कर सकता है और इसको दूसरों तक भी बेहतर अंदाज़ में पहुँचा सकता है।
क्या हर शरई आदेश ‘मस्लहत’ पर आधारित है?
और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है। वह यह है कि क्या शरीअत के आदेशों में हर आदेश के पीछे अनिवार्य रूप से कोई-न-कोई ‘मस्लहत’ और तत्वदर्शिता मौजूद है। क्या सर्वोच्च अल्लाह ने जो आदेश दिए हैं वह हमारी किसी तत्वदर्शिता और ‘मस्लहत’ की ख़ातिर दिए हैं या उनके पीछे कोई निर्धारित तत्वदर्शिता और ‘मस्लहत’ नहीं है और उनका उद्देश्य केवल इसलिए सृष्टि के रचयिता के तशरीई आदेशों की पैरवी कराना है कि यह दिखाया जाए कि कौन-सा बंदा आदेश का पालन करता है और कौन-सा नहीं करता। अगर केवल यही परीक्षा लेना अभीष्ट हो तो फिर व्यक्तिगत आदेशों में अलग-अलग हिकमतें तलाश करने के बजाय पहले ही यह मान लिया जाए कि सर्वोच्च अल्लाह ने जो आंशिक आदेश दिए हैं वे बिना किसी व्यक्तिगत तत्वदर्शिता के दिए हैं। इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों की राय यह रही है कि सर्वोच्च अल्लाह के आदेशों के पीछे कोई अलग-अलग तत्वदर्शिता या ‘मस्लहत’ पाया जाना ज़रूरी नहीं है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में जो बात कही जाती है वह यह है कि सर्वोच्च अल्लाह किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। उसके आदेशों को किसी तत्वदर्शिता या ‘मस्लहत’ का पाबंद समझना उसके वास्तविक स्वामी और सर्वशक्तिमान होने की धारणा के ख़िलाफ़ है। तत्वदर्शिताओं की पाबन्दी करना और निहितार्थों का ध्यान रखना तो हम बंदों का काम है। इसलिए कि हम मुहताज और ज़रूरतमन्द हैं। इसलिए हम बन्दे होने की हैसियत से कोई ऐसा काम करने के अधिकारी नहीं हैं जो किसी तत्वदर्शिता पर आधारित न हो। लेकिन सर्वोच्च अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है। वह इस बात का पाबंद नहीं है कि कोई चीज़ उसी समय पैदा करे जब उसके पीछे कोई ‘मस्लहत’ हो। ‘मस्लहत’ की पाबन्दी तो मजबूर प्राणी करता है। सीमित क्षमता रखनेवाला व्यक्ति करता है। जिसका आदेश, जिसकी हुकूमत, जिसकी सत्ता और जिसकी तत्वदर्शिता, जिसका काम, हर चीज़ असीमित हो, वह किसी चीज़ का पाबंद कैसे हो सकता है।
वास्तविकता यह है कि तौहीद (एकेश्वरवाद) की वास्तविकता के दृष्टिकोण से यह राय बड़ी मज़बूत मालूम होती है। ‘अशाइरा’ जो मुसलमानों में इलमे-कलाम के बहुत-से विशिष्टतम चिन्तकों का एक प्रसिद्ध मसलक है, वे इसी बात को मानते हैं। इमाम राज़ी का दृष्टिकोण यही है। इमाम ग़ज़ाली ने अपनी रचनाओं में और इमाम राज़ी ने क़ुरआन की अपनी टीका में बड़े असाधारण जोश और पुर-ज़ोर तर्कों से इस बात को जगह-जगह बयान किया है। इमाम राज़ी, इमाम ग़ज़ाली और उनके हम-ख़याल लोगों का कहना यह है कि शरीअत के आदेशों की हैसियत लगभग इस तरह की है। समझाने के लिए वह बिना उपमा के कहते हैं कि जैसे आपके दो नौकर हों। एक के बारे में आपको सन्देह हो कि वह आपका आज्ञाकारी नहीं है। और उसकी आज्ञाकारिता को जाँचने के लिए आप उसको कोई आदेश दें। यहाँ आप उस अवज्ञाकारी नौकर को कोई भी आदेश दे सकते हैं। इस आदेश में अपने-आपमें किसी तत्वदर्शिता का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उद्देश्य केवल यह है कि स्पष्ट हो जाए कि यह नौकर कितना आज्ञाकारी है। इसी तरह उदाहरणार्थ किसी नौकर की ईमानदारी को आप जाँचना चाहें और घर में किसी जगह चुपके-से कुछ रक़म रख दें और देखें कि यह नौकर आँख बचाकर आपकी रक़म उठाता है कि नहीं उठाता। अब वहाँ रक़म रखने में अपने-आपमें कोई तत्वदर्शिता नहीं है। वहाँ रक़म रखना या न रखना एक आम-सी बात है जिसमें कोई और तत्वदर्शिता या ‘मस्लहत’ होना ज़रूरी नहीं। अस्ल उद्देश्य यह जानना है कि वह नौकर ईमानदार है कि नहीं। इमाम राज़ी और उनके साथी फ़ुक़हा का कहना है कि शरीअत के आदेशों में बस इसी तरह की ‘मस्लहत’ है। इससे बढ़कर कोई और तत्वदर्शिता या इंसानों के लिए कोई और फ़ायदा पाया जाना ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिरिया का भी यही मसलक है जिनका मैंने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था।
शरीअत की तत्वदर्शिता पर महत्वपूर्ण किताबें
लेकिन मुसलमानों में विद्वानों एवं चिन्तकों की बहुत बड़ी संख्या मुतकल्लिमीने-इस्लाम (इस्लामी धारणाओं को बौद्धिक एवं तार्किक रूप से सिद्ध करनेवाले) और तत्वदर्शियों की अधिकांश संख्या, इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों), मुहद्दिसीन और क़ुरआन की व्याख्या करनेवालों की बहुसंख्या का कहना यह है कि शरीअत के आदेशों के पीछे बहुत-सी मस्लहतें और हिकमतें मौजूद हैं। और वे मस्लहतें इंसान के कल्याण, इंसान की सफलता और कामयाबी, इंसान के जीवन में सन्तुलन की प्राप्ति, इंसान की जान-माल की सुरक्षा और ऐसी ही बहुत-सी दूसरी तत्वदर्शिताओं की प्राप्ति है। यह वे मस्लहतें हैं जो शरीअत के आदेशों में सर्वोच्च अल्लाह ने सामने रखी हैं।
मुसलमान चिन्तकों की बहुसंख्या का यही विचार है। इस विषय में जिन लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, उनमें से तीन बल्कि चार अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का नाम मैं लूँगा। अगर आपको अरबी आती हो तो ये तीन किताबें ज़रूर पढ़ें।
एक किताब तो अल्लामा इज़ुद्दीन-बिन-अब्दुस्सलाम की है। यह अपने ज़माने के बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े शाफ़िई फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) थे। इतने बड़े फ़क़ीह थे कि उनकी उपाधि ‘सुल्तानुल-उलमा’ थी। मिस्र के चीफ़ जस्टिस थे। उन्होंने ‘क़वाइदुल-अहकाम फ़ी मसालेहुल-अनाम’ के नाम से दो भागों में एक किताब लिखी है। कोई पाँच सौ पृष्ठों की किताब है। इस में उन्होंने अत्यन्त वज़नी और बौद्धिक तर्कों के साथ अत्यन्त तार्किक और बौद्धिक ढंग से क़ुरआन और सुन्नत से उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट की है कि शरीअत के हर आदेश के पीछे कोई-न-कोई ‘मस्लहत’ और कोई-न-कोई तत्वदर्शिता पाई जाती है।
दूसरी किताब जो इस विषय पर बड़ी मौलिक किताब है वह फ़िक़्हे-हंबली के एक बड़े प्रसिद्ध फ़क़ीह अल्लामा इब्ने-क़य्यिम की है। उनका नाम आपमें से अक्सर ने सुना होगा। वह अल्लामा इब्ने-तैमिया के शिष्य हैं। और न केवल फ़िक़्हे-हंबली, बल्कि फ़िक़्हे-इस्लामी के अति नामवर और अति सम्माननीय उलमा में से हैं। उनकी किताब है ‘आलामुल-मूक़िईन’ इसमें उन्होंने तर्कों से साबित किया है कि शरीअत के हर आदेश की अस्ल न्याय की तत्वदर्शिता है। पूरे न्याय का लागू होना, पूरा इंसाफ़ शरीअत के आदेशों का मूल उद्देश्य है। एक-एक चीज़ का तर्क देकर यह दिखाया है कि शरीअत का हर आदेश न्याय पर आधारित है। उनकी यह बौद्धिकतापूर्ण किताब चार मोटे भागों में लिखी गई है। जो व्यक्ति भी इस किताब को समझकर पढ़ता है वह सन्तुष्ट मन से यह बात कह सकता है कि इस्लामी शरीअत में न्याय का अत्यन्त ध्यान रखा गया है।
तीसरी किताब जो पूरे मानव इतिहास में अपने प्रकार की निराली किताब है और इस्लामी इतिहास में क़ानून दर्शन में आज तक इससे बेहतर किताब नहीं लिखी गई है, बल्कि अगर यह कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा कि किसी क़ौम में, किसी सभ्यता में और किसी क़ानूनी परम्परा में क़ानून दर्शन पर इससे बेहतर और भरपूर किताब मौजूद नहीं है। यह किताब प्रसिद्ध मालिकी फ़क़ीह इमाम अबू-इसहाक़ शातबी की ‘अलमुवाफ़क़ात फ़ी उसूलिश-शरीआ’ है जो चार भागों में है। इस किताब में इमाम शातबी ने अपने ज़माने तक के क़रीब-क़रीब तमाम ज्ञान-विज्ञान से काम लिया है और तार्किक और बौद्धिक तर्कों से यह साबित कर दिया है कि शरीअत के हर आदेश के पीछे एक ‘मस्लहत’ है। और वह अमुक ‘मस्लहत’ है।
चौथी किताब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अमीरुल-मोमिनीन फ़िल-हदीस हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी की प्रसिद्ध किताब ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ है। इस किताब में शाह साहब ने शरीअत की तत्वदर्शिता की पूरे व्यवस्था को एक नए और अनोखे ढंग से पेश किया है।
शरीअत के आदेशों की हिकमतें
इसलिए यह बात तो स्पष्ट हो गई कि शरीअत के हर आदेश में कोई-न-कोई वजह कोई-न-कोई तत्वदर्शिता और ‘मस्लहत’ छिपी है। स्वयं पवित्र क़ुरआन पर ग़ौर करने से कुछ आदेशों की हिकमतें हमारे सामने आ जाती हैं। पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह वे मस्लहतें बयान की हैं। उदाहरणार्थ एक जगह यह उल्लेख है कि अल्लाह ने पैग़ंबर क्यों भेजे। पैग़म्बरों के भेजे जाने की तत्वदर्शिता के तौर पर बताया गया कि “ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों के पास अल्लाह के यहाँ पेश करने के लिए कोई तर्क शेष न रहे।” दूसरे शब्दों में कोई इंसान क़ियामत के दिन यह न कह सके कि “ऐ परवरदिगार! मुझे मालूम नहीं था कि आपका आदेश और तरीक़ा क्या है।” इसलिए न मैंने आपकी इबादत की और न आपकी मर्ज़ी पर चलने की कोशिश कर सका। लेकिन पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) के तशरीफ़ लाने और दीन एवं शरीअत का विसतृत विवरण पहुँचा दिए जाने के बाद किसी के लिए यह कहना अब सम्भव नहीं रहा। अब किसी इंसान के लिए यह कहना सम्भव नहीं होगा कि ऐ अल्लाह! मैं नहीं जानता था कि तेरी तत्वदर्शिता या तेरी शरीअत क्या थी। तेरे आदेश क्या थे। तेरी ख़ुशी और नाराज़गी किस चीज़ में थी। अब शरीअत के आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) ने अल्लाह की नियति और मर्ज़ी को आम कर दिया है। गोया अल्लाह ने पैग़म्बरों को अकारण नहीं भेजा है, बल्कि तर्क पूरा करने के लिए भेजा है। अगरचे इंसान को बुद्धि दी है और उसके चारों ओर ऐसे सुबूत एवं तर्क पैदा कर दिए हैं कि वह उनकी सहायता से और अपनी बुद्धि से काम लेकर अल्लाह के अस्तित्व को मालूम कर सकता है, लेकिन मात्र मानव-बुद्धि पर, मात्र सुबूतों पर और मात्र घटनात्मक गवाहियों पर सर्वोच्च अल्लाह ने बस नहीं किया, बल्कि पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) को भेजा। एक दो नहीं हज़ारों नहीं, एक लाख चौबीस हज़ार व्यक्तियों को भेजा। अब तर्क देने का कार्य पूरा हो गया।
पवित्र क़ुरआन में एक जगह यह बहस है कि हमने जीवन और मृत्यु का यह सिलसिला क्यों पैदा किया है। वैसे तो सर्वोच्च अल्लाह स्रष्टा है जिसको चाहे पैदा करे, जिसको चाहे पैदा न करे। कौन पूछ सकता है कि किसी को पैदा क्यों किया और किसी को पैदा क्यों न किया गया। लेकिन सर्वोच्च अल्लाह ने स्वयं जन्म और मरण के इस सिलसिले की तत्वदर्शिता बयान करते हुए कहा कि “ताकि सर्वोच्च अल्लाह आज़माकर दिखाए कि कौन अच्छे कर्म करनेवाला है” (क़ुरआन, 67:2) और कौन बुरा कर्म करनेवाला। यानी अमल की अच्छाई और बुराई में लोगों की परीक्षा लेना अभीष्ट है। यह पूरा जीवन परीक्षा है और इस परीक्षा की वजह से इंसानों के लिए ये सारे मामले और परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं।
एक जगह कहा गया है कि “मैंने जिन्नों और इंसानों को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत करें।” (क़ुरआन, 51:56) गोया अल्लाह की इबादत इंसान अपने फ़ैसले और अपनी आज़ाद मर्ज़ी और रुचि तथा शौक़ से कितनी करता है, यह दिखाना अभीष्ट है। मजबूरी में तो सारी सृष्टि अल्लाह के आदेशों की पैरवी करती है। अल्लाह के तकवीनी अहकाम (प्राकृतिक नियमों) के पाबंद तो चाँद, सूरज, सितारे और सब ही हैं। जिस तरह भी, जब भी और जो भी अल्लाह का आदेश होता है, बिलकुल उसी तरह ये चीज़ें काम कर रही हैं। नदियाँ भी अल्लाह के आदेशों का पालन कर रही हैं। रेगिस्तान के ज़र्रे भी कर रहे हैं, पहाड़ों के पत्थर भी कर रहे हैं। जानवर और परिंदे भी कर रहे हैं। लेकिन इंसान अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शरीअत के आदेशों का कितना पालन करता है, यह इंसानों और अल्लाह की दूसरी रचनाओं को बताना और दिखाना अभीष्ट था।
ये तो इस बात के उदाहरण थे कि आम तौर पर सृष्टि के जन्म के पीछे अल्लाह की एक बड़ी हिकमत और ‘मस्लहत’ कार्यरत है। इस बड़ी तत्वदर्शिता के तहत जितने आदेश होंगे वे इस बड़ी तत्वदर्शिता के तहत आएँगे। अब अगर आंशिक आदेशों में आंशिक हिकमतें न भी पाई जाएँ तो कोई हरज नहीं, क्योंकि बड़ी तत्वदर्शिता मौजूद है, इसके होते हुए आंशिक तत्वदर्शिता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर आदेश की आंशिक तत्वदर्शिता भी रखी गई है। इस बड़ी और सामान्य तत्वदर्शिता के अलावा आंशिक हिकमतें भी हर आदेश में पाई जाती हैं।
उदाहरण के रूप में नमाज़ के बारे में कहा गया कि “नमाज़ अश्लील और बुरे कामों दोनों से रोकती है।” (क़ुरआन, 29:45) ‘फ़ुहशा’ (अश्लीलता) इस बुराई को कहते हैं जिसका मूल उद्देश्य इंसान के दिल में हो, ‘मुनकर’ वह बुराई है जिसका नुक़्सान समाज में ज़ाहिर होता हो। गोया ‘फ़ुहशा’ से अभिप्रेत छिपी बुराई और ‘मुनकर’ से अभिप्रेत खुली बुराई है। यों छिपी और खुली हर प्रकार की बुराई से अल्लाह ने मना किया है और इसको रोकने में नमाज़ बड़ी सहायक सिद्ध होती है। यह नमाज़ की एक नैतिक और आध्यात्मिक तत्वदर्शिता है। रोज़े के बारे में कहा गया कि “यह तुम्हारे अन्दर तक़्वा (ईशपरायणता) पैदा करने के लिए है।” ज़कात के बारे में कहा गया कि यह तुम्हारे माल और स्वामित्व एवं धनाढ्यता की भावना को पवित्र करती है। हज के बारे में बताया गया कि इससे तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसकी निशानियों की याद पैदा होगी। ‘फ़ै’ के माल के जो आदेश बताए गए हैं उनकी तत्वदर्शिता यह बताई गई है कि पूरे देश और समाज का धन-दौलत एक जगह संकेन्द्रित होकर न रह जाए। क़िसास की तत्वदर्शिता यह बताई गई कि तुम्हारे जीवन का दारोमदार एक-दूसरे के जान-माल के सम्मान पर है, और जान के सम्मान का आधार क़िसास के आदेशों पर है।
आयते-मदाइना (सूरा-2:282) में लेन-देन और क़र्ज़ के आदेश बताए गए हैं। लेन-देन और क़र्ज़ के मामलों के बारे में पवित्र क़ुरआन की सूरा-2 बक़रा में जो आदेश दिए गए हैं, उनके बारे में कहा गया है कि “यह न्याय एवं इंसाफ़ के ज़्यादा क़रीब है” कि तुम इस तरह का मामला करो। न्याय एवं इंसाफ़ की पैरवी तुम्हारे लिए भी आसान होगी और तुम्हारे दूसरे पक्ष के लिए भी आसान होगी। दस्तावेज़ लिखने का आदेश दिया गया कि सम्भव हो तो लिख दो कि किसका ‘हक़’ कितना बनता है। इसकी तत्वदर्शिता यह बताई गई कि “तुम्हें कोई शक-सन्देह नहीं होगा” कि दूसरे ने मेरा ‘हक़’ तो नहीं मार लिया।
कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अत्यन्त ईमानदार आदमी के बारे में आपका ख़याल होता है कि आपने उसकी देय रक़म चुका दी है और उसके जो पैसे आपकी तरफ़ बनते थे वे आपने दे दिए हैं। लेकिन इसका ख़याल होता है कि आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं। अब दोनों तरफ़ एक बद-गुमानी और ग़लत-फ़हमी शेष रह जाती है। आपको हमेशा यह ग़लत-फ़हमी रहेगी कि आदमी तो बड़ा ईमानदार बनता था, लेकिन मुझसे दो बार पैसे ले लिए। मैंने पहले ही अदा कर दिए थे, लेकिन यह साहब पैसे लेकर बाद में मुकर गए कि मैंने नहीं लिए और दोबारा पैसे ले लिए। सम्भव है आपने एक ही बार दिए हों और आपकी याददाश्त ग़लती कर रही हो। यह भी हो सकता है कि उसके दिल में भी बद-गुमानी पैदा हो कि यों तो बड़े ईमानदार बनते थे, लेकिन अब मेरे पैसे देने से इनकार कर गए थे और अगर मैं स्वयं न ले लेता तो उसको नहीं देने थे। यों यह बद-गुमानी दोनों के दिलों में हमेशा रहेगी। बद-गुमानी बहुत बुरी चीज़ है। इससे दिलों में खोट पैदा हो जाता है, सम्बन्ध में बिगाड़ आ जाता है और कभी-कभी दुश्मनियाँ तक पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर आप क़र्ज़ का मामला लिखित में ले आएँ तो इस बद-गुमानी से बचने का मौक़ा मिल जाएगा। सम्भव है आप थोड़ी रिआयत और झिझक की वजह से पैसे न लें। और अगर आपने पैसे रिआयत में नहीं लिए तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आपने ख़ुशी से छोड़ दिए। दूसरे पक्ष के लिए इस तरह पैसे लेना जायज़ नहीं होगा। इन तमाम समस्याओं और मुश्किलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि शक और बद-गुमानी से बचने का पहले ही दिन प्रबन्ध कर लो और इन नतीजों से बचने के लिए यह मामला लिख लो। अगर लिखोगे तो याददाश्त पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। यह वह हिकमत है जिसकी तरफ़ इशारा करते हुए लिखने की ताकीद की गई।
हाथ काटने का आदेश दिया गया है कि चोर चोरी का जुर्म करे तो उसका हाथ काट दो। इस सख़्त सज़ा की तत्वदर्शिता यह बताई गई कि “अल्लाह की ओर से उनको शिक्षाप्रद सज़ा दी जाए” और उन्होंने जो नाजायज़ कमाई की है उसका बदला उन्हें मिलना चाहिए। पर्दे के बारे में कहा गया कि “जो बदकार और चरित्रहीन लोग हैं उनको पता चल जाए कि यह बाइज़्ज़त महिलाएँ हैं, इसलिए उनको अकारण तंग न करें।” हिजाब और शालीन वस्त्रों से यह फ़ायदा ख़ुद-ब-ख़ुद प्राप्त हो जाता है कि नैतिक आचरण, किरदार और हया की रक्षा हो जाती है। यह उन तत्वदर्शिताओं के कुछ छोटे-छोटे उदाहरण हैं जो पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह बयान हुए हैं।
हदीसों का एक सरसरी जायज़ा लें तो वहाँ भी हर आदेश के पीछे कोई-न-कोई तत्वदर्शिता बयान हुई है। अगर आपके पास समय हो तो भारतीय उपमहाद्वीप के अमीरुल-मोमिनीन फ़िल-हदीस हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ ज़रूर पढ़ लीजिए। इस किताब के उर्दू और अंग्रेज़ी अनुवाद उपलब्ध हैं। ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ के दूसरे भाग में हज़रत शाह वलियुल्लाह साहब ने हदीसों में बयान किए हुए बहुत-से आदेशों की मस्लहतें और उनकी हिकमतें बयान की हैं।
लेकिन एक मुसलमान अगर इन सब आदेशों की पैरवी करता है जो उसको अवश्य ही करनी चाहिए, वह केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। किसी ‘मस्लहत’ या तत्वदर्शिता के लिए नहीं करनी चाहिए। नमाज़ इसलिए पढ़ना कि यह मुझे चरित्रहीनता से रोकेगी तो मैं अच्छे किरदारवाला प्रसिद्ध हो जाऊँगा। अच्छे किरदारवाला प्रसिद्ध हो जाऊँगा तो मेरी शोहरत अच्छी होगी और नेक-नामी और बढ़ेगी, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सत्कर्म का उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर इंसान इन आदेशों का उनकी सही आत्मा के साथ पालन करेगा तो लाभ और मस्लहतें ख़ुद-ब-ख़ुद प्राप्त हो जाएँगी।
ग़रज़ शरीअत के आदेशों के पीछे यह और इस तरह की अनगिनत हिकमतें हैं जो पवित्र क़ुरआन में सैंकड़ों और हदीसों में हज़ारों बार बयान हुई हैं। इन सब पर जब इस्लाम के महाविद्वानों ने ग़ौर किया तो उन्होंने महसूस किया कि इन सब तत्वदर्शिताओं का सार और जड़ एक मौलिक तत्वदर्शिता और मूल ‘मस्लहत’ में छिपा है। और यह वह तत्वदर्शिता और ‘मस्लहत’ है जो पवित्र क़ुरआन की सूरा-57 हदीद में बयान हुई है। सूरा-57 हदीद की यह आयत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयतों में से है। पवित्र क़ुरआन में मौलिक सिद्धान्त जिन आयतों में बयान हुए हैं उन आयतों में भी जो अत्यन्त मौलिक महत्व रखनेवाली आयत है, वह यह है कि “हमने अपने पैग़म्बरों को स्पष्ट निशानियाँ देकर भेजा। उनके साथ किताब और मीज़ान (तुला) अवतरित की ताकि लोग मुकम्मल न्याय एवं इंसाफ़ पर क़ायम हो जाएँ।” (क़ुरआन, 57:25) अत: लोगों का वास्तविक और पूरे न्याय और इंसाफ़ के आधार पर क़ायम हो जाना, यह तमाम आसमानी किताबों का मौलिक उद्देश्य था और यही तमाम नबियों (अलैहिमुस्सलाम) का इस जीवन के हवाले से मौलिक लक्ष्य था। अल्लाह की तमाम शरीअतों और आसमानी किताबों की तमाम-तर शिक्षा का गंतव्य स्थान यही था कि यहाँ इस सांसारिक जीवन में लोगों को न्याय एवं इंसाफ़ पर क़ायम कर दिया जाए।
न्याय और इंसाफ़
यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि पवित्र क़ुरआन ने इस आयत में ‘अद्ल’ (न्याय) नहीं बल्कि ‘क़िस्त’ का शब्द प्रयुक्त किया है। पवित्र क़ुरआन में अद्ल और इंसाफ़ का अर्थ बयान करने के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक अद्ल और दूसरा क़िस्त। दोनों के अर्थ इंसाफ़ के हैं। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये दोनों शब्द बिलकुल समानार्थी हैं। अगर ये दोनों समानार्थी हैं तो फिर दूसरा सवाल यह सामने आता है कि क्या पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द आए हैं। यह एक बड़ी लंबी बहस है और विद्वानों ने इस सवाल पर पूरी-पूरी किताबें लिखी हैं कि क्या पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जबकि कुछ लोगों की राय में पर्यायवाची शब्द पवित्र क़ुरआन में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। जिन लोगों का कहना है कि पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं हुए उनका मत है कि पवित्र क़ुरआन में कोई ग़ैर-ज़रूरी और फ़ालतू शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि “ला अ-ब-स फ़िश-शरीआ।” यह एक उसूल है कि शरीअत में कोई चीज़ फ़ालतू और बेकार नहीं है। पवित्र क़ुरआन ही अस्ल शरीअत है। इसमें अगर एक शब्द भी ग़ैर-ज़रूरी और अधिक है तो वह फ़ालतू और बेकार है। सर्वोच्च अल्लाह के कलाम में कोई शब्द बेकार नहीं आ सकता। अत: पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द भी नहीं हो सकते।
यह एक राय है। दूसरी राय यह है कि पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द आए हैं। उदाहरणार्थ नबी और रसूल, क़िस्त और अद्ल और ऐसे बहुत-से शब्द हैं जो बज़ाहिर एक ही अर्थ के हैं। और इन दोनों का अर्थ एक ही मालूम होता है। सच्चाई यह है कि इस विषय पर विद्वान चिन्तन-मनन करते रहे हैं। जहाँ-जहाँ ये पर्यायवाची शब्द आते गए उन आयतों पर ख़ास तौर से ग़ौर किया गया। इसपर एक राय यह क़ायम हुई कि पवित्र क़ुरआन में पर्यायवाची शब्द हैं भी और नहीं भी हैं। दोनों बातें एक ही समय में दुरुस्त हैं। आप कहेंगे कि एक साथ दोनों बातें कैसे सही हैं। मेरा जवाब यह होगा कि दोनों बातें इस तरह दुरुस्त हैं कि क़ुरआन की टीका के शोधपरक विद्वानों ने इन दोनों मतों को एक मौलिक सिद्धान्त में जमा कर दिया है। वे कहते हैं कि “जब दो ऐसे शब्द जो बज़ाहिर समानार्थी हों और पवित्र क़ुरआन में एक ही जगह यानी एक ही आयत या एक ही सन्दर्भ में आएँ तो उनके अर्थ अलग-अलग माने जाएँगे। और अगर अलग-अलग सन्दर्भ में ये शब्द प्रयुक्त हुए हों तो इन दोनों के एक ही अर्थ हो सकते हैं और वे समान हो सकते हैं। उदाहरणार्थ पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है कि “हमने न कोई रसूल भेजा न कोई नबी”, जिसके साथ ऐसा और ऐसा मामला न हुआ हो। यहाँ एक ही अर्थ के दो अलग-अलग शब्द एक जगह आए हैं, अत: इस नियम के अनुसार यहाँ इन दोनों के अर्थ अलग-अलग होंगे। और जहाँ-जहाँ यह शब्द अलग-अलग आए हैं तो वहाँ नबी रसूल के अर्थ में और रसूल नबी के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है।
इसी तरह से पवित्र क़ुरआन में अद्ल और क़िस्त के शब्द जहाँ एक जगह, एक आयत में या किसी एक सन्दर्भ में आए हैं वहाँ दोनों का अर्थ अलग-अलग है। और जहाँ अलग-अलग आए हैं वहाँ उनका अर्थ अलग-अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। अद्ल के ज़ाहिरी अर्थ हैं कि ऊँट या किसी और बोझ ढोनेवाले जानवर पर बोझ लादते समय बोझ को दो बराबर भागों में विभाजित करके रखना। जब ऊँट पर बोझ लादा जाता है तो दोनों तरफ़ का बोझ आकार और वज़न में लगभग एक जितना होता है। अगर दोनों तरफ़ का आकार और वज़न एक जैसा न हो तो ऊँट के चलने के अंदाज़ और रफ़्तार पर-प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया को अरबी भाषा में अद्ल कहते हैं। गोया अद्ल का अर्थ है कि ज़ाहिरी तौर पर दो चीज़ों को इस तरह बराबर कर दिया जाए कि देखने में दोनों बराबर हो जाएँ। गोया तराज़ू के दो पलड़े बराबर हो गए। दोनों पक्षों का मत सुनने के बाद ज़ाहिरी तर्क पर आपने फ़ैसला कर दिया और दोनों का मत ज़ाहिरी तौर पर अपनी-अपनी जगह दुरुस्त हो गया। यह अद्ल है।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो फ़ैसला या क़दम ज़ाहिरी तौर पर अद्ल हो वह वास्तविक रूप से भी अद्ल हो। इसलिए कि हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर आपसे एक चीज़ के समझने में ग़लती हुई हो और वास्तविकता इससे विभिन्न हो। अत: अगर वास्तविकता ज़ाहिर से भिन्न होगी तो अद्ल नहीं होगा। ज़ाहिरी अद्ल तो घटित हो जाएगा, लेकिन वास्तविक अद्ल क़ायम नहीं होगा। इस अन्तर को स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान किया है। एक प्रसिद्ध हदीस है जो अनेक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से उल्लिखित है। यह उन हदीसों में से है जो सिहाह सित्ता (प्रमाणित हदीसों की छः किताबें) की पाँच किताबों में आई हैं। बहुत थोड़ी हदीसें हैं जो सिहाह सित्ता की हर किताब में आई हों। इस तरह जो सिहाह सित्ता में से पाँच में आई हों वे भी कम हैं। यह हदीस उनमें से एक है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में दो सहाबी तशरीफ़ लाए। दोनों के दरमियान एक ज़मीन की मिल्कियत के बारे में कोई मतभेद था। दोनों का कहना यह था कि ज़मीन के मालिक वे हैं और ज़मीन उनकी है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दोनों की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने उनमें से एक के पक्ष में फ़ैसला सुना दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क़ाज़ी-अलक़ुज़ा (चीफ़ जस्टिस) होने के साथ-साथ नबी और रसूल भी थे। नबी का काम केवल ज़ाहिरी फ़ैसले करना नहीं, बल्कि उम्मत को शिक्षा देना, उम्मत को शरीअत प्रदान करना और आइन्दा रहती दुनिया तक मानवता के लिए मार्गदर्शन का सामान करना भी था। आपने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को जमा किया। इन दोनों सहाबियों को भी बुलाया। फिर आपने फ़रमाया कि “तुम लोग मेरे पास अपने मुक़द्दमे लेकर आते हो, हो सकता है कि तुममें से कोई दूसरे से ज़्यादा वाकपटु हो, बात करने में तेज़ हो। मुझे अपनी वाकपटुता और बातचीत से प्रभावित कर दे और मैं उसके पक्ष में फ़ैसला दे दूँ, जबकि ‘हक़’ उसका न बनता हो और विवादित चीज़ उस वाकपटु व्यक्ति की न हो, बल्कि दूसरे पक्ष की हो। तो अगर ऐसा है तो वह चीज़ जो मेरे द्वारा सर्वोच्च अल्लाह तुम्हें दे रहा है, यह जहन्नम की आग का एक टुकड़ा है। अत: जिसका ‘हक़’ बनता है उसको दे दो।”
अब आप देखें कि ज़ाहिरी इंसाफ़ और हक़ीक़ी इंसाफ़ दोनों में अन्तर बिलकुल स्पष्ट हो गया। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़ैसला किया है, आपसे बढ़कर अद्ल और इंसाफ़ की क्या कल्पना की जा सकती है। जिनके बारे में यह सोचा तक नहीं जा सकता कि उन्होंने किसी एक पक्ष की तरफ़दारी की हो, अल्लाह की पनाह! या किसी पक्ष के साथ नाइंसाफ़ी की होगी। इसके बावजूद कि अद्ल और क़ानून के तमाम तक़ाज़े पूरे किए गए। ज़ाहिरी तौर पर इंसान के बस में जो कुछ है वह सब पूरा कर दिया गया। लेकिन दिलों का हाल तो क़ाज़ी नहीं जानता। दिलों का हाल तो केवल अल्लाह जानता है। अब अगर वास्तविकता की दृष्टि से वह व्यक्ति मालिक नहीं था और किसी ग़लत गवाही या ग़लत सुबूत के आधार पर उसने अपने पक्ष में फ़ैसला ले लिया, तो इससे यह न समझो कि वास्तविकता की दृष्टि से भी यह तुम्हारे लिए जायज़ हो गया, बल्कि सच तो यह है कि यह जहन्नम का एक टुकड़ा है जो तुमको मिला है और तुमको क़ियामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। यह जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बाद में आदेश दिया यह हक़ीक़ी इंसाफ़ क़ायम करने का आदेश है जो आपने सम्बन्धित पक्ष को दिया।
आज की दुनिया एक लम्बे सफ़र के बाद इस वास्तविकता तक पहुँची है कि इंसाफ़ की दो क़िस्में हैं। क़ानूनी इंसाफ़ और वास्तविक इंसाफ़। कभी-कभी यह हो सकता है कि क़ानूनी इंसाफ़ के परिणामस्वरूप हक़ीक़ी इंसाफ़ न हुआ हो। इस्लामी शरीअत ने पहले दिन से मामलात के दो पहलू रखे। एक पहलू ‘एतिबारे-क़ज़ाई’ और दूसरा पहलू ‘एतिबारे-दियानी’ कहलाता है। फ़िक़्ह की किताबों में आपको जगह-जगह मिलेगा कि ‘यजूज़ि दियानतन’, ‘यजूज़ि क़ज़ाअन’। यानी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मामले का वास्तविक आदेश कोई और हो, लेकिन अदालत का फ़ैसला कुछ और हो। इसलिए कि अगर आपके दिल में कोई और चीज़ थी, जिसका क़ानूनी दस्तावेज़ात और ज़ाहिरी सुबूतों से अनुमान नहीं हो सकता था तो अदालत तो ज़ाहिरी सुबूतों के अनुसार ही फ़ैसला करेगी। आपके दिल में जो कुछ था वह तो आप ही को बेहतर मालूम है।
मान लीजिए, एक महिला के पति ने उसको तलाक़ दे दी। यह मसला आए दिन हम सबके सामने आता है, इसलिए मैं इसका उदाहरण देता हूँ। पति और पत्नी दोनों को ख़ूब मालूम है कि तलाक़ हो गई। और तलाक़ की जो भी शर्तें होती हैं वे सब पूरी हो गई हैं। आज तलाक़ दे दी, फिर एक महीने बाद दूसरी दे दी, फिर दो महीनों बाद तीसरी दे दी। एक-एक महीने के अन्तराल से कई महीनों के दौरान तीन तलाक़ें दे दीं। यह मुसलमानों के हर फ़क़ीह के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह (सर्वसम्मत) मसला है और इसमें कोई शक-शुब्ह नहीं कि अब दोनों के दरमियान पूरी तरह सम्बन्ध समाप्त हो गया। अब अगर दोनों बदनीयती पर उतर आएँ और इसको छिपा लें। न कोई गवाह है न कोई सुबूत है और न कोई दस्तावेज़ है। अब अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाकर शिकायत करे तो कोई अदालत इस स्थिति में तलाक़ हो जाने का फ़ैसला नहीं देगी। कोई मुफ़्ती उसका फ़तवा नहीं देगा। इसलिए कि कोई गवाही, कोई सुबूत या दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। इसलिए क़ानूनी रूप से हर अदालत यह कहेगी कि निकाह बाक़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में निकाह शेष नहीं रहा और दोनों को मालूम है और वे जानते हैं कि अस्ल मामला किया है। अगर वे दोनों उसको छिपाते हैं तो दुनिया की नज़रों के लिहाज़ से तो वे पति-पत्नी हैं, लेकिन वास्तव में शरीअत के आदेश की दृष्टि से अब बिलकुल ग़ैर हैं। अब वे ख़ुद से शरीअत के आदेशों पर अमल दरआमद नहीं करेंगे, तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। यह है क़ानूनी और वास्तविक इंसाफ़ में अन्तर।
पवित्र क़ुरआन ने यहाँ “लियक़ौमिन-नासि बिल-क़िस्त” का शब्द प्रयुक्त किया है। (ताकि लोग वास्तविक इंसाफ़ पर क़ायम हो जाएँ) वास्तविक और अदालती इंसाफ़, यह इंसाफ़ की दो सतहें हैं। एक सतह की ज़िम्मेदार तो अदालतें, राज्य और राज्य की संस्थाएँ हैं। दूसरी सतह के ज़िम्मेदार स्वयं व्यक्ति हैं, जिनको सही स्थिति का ज्ञान होता है और वे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। शरीअत के हर आदेश का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य यही एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए पाँच चीज़ों की रक्षा ज़रूरी है। ये पाँच चीज़ें शरीअत के उद्देश्य कहलाती हैं।
शरीअत के पाँच मौलिक उद्देश्य
1. दीन की रक्षा
सबसे पहला उद्देश्य दीन की रक्षा है। दीन से मुराद यह है कि अल्लाह और बन्दे के दरमियान जो ख़ास रिश्ता है, अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध का जो प्रकार है, जिसकी सीमाबन्दी और निर्धारण पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से होती है। जिसको संगठित करने के लिए पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में अनगिनत आदेश दिए गए हैं। नमाज़ का आदेश, रोज़े का आदेश, तिलावत (क़ुरआन पाठ) का आदेश, अल्लाह को याद रखने का आदेश, ज़िक्र का आदेश। इन तमाम चीज़ों का उद्देश्य यह है कि अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध बना रहे। और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास बन्दे के दिल में जागृत रहे। फिर दीन की शिक्षा में इस ख़ास और मौलिक दायरे से बाहर भी कई दायरे हैं जिनका उद्देश्य बन्दे और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध को संगठित करना है, जिनका उद्देश्य बन्दे और उसके चारों ओर जो विस्तृत एवं विशाल दुनिया फैली हुई है उसमें ज़िम्मेदारियाँ निभाने और इस दुनिया को सही तौर पर बरतने के लिए बंदों को तैयार करना है। इन सब दायरों की सुरक्षा और इस पूरी शिक्षा की रक्षा शरीअत के आदेशों का सबसे पहला उद्देश्य है। आप पवित्र क़ुरआन आरम्भ से लेकर अन्त तक पढ़ें। हदीसों के संग्रहों का आरम्भ से लेकर अन्त तक अवलोकन करें। फ़िक़्ह की किताबों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति की ख़ातिर हज़ारों की संख्या में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से आदेश मौजूद हैं। फ़िक़्ह की किताब में अगर यह लिखा हुआ है कि पानी कैसे पाक होता है और कैसे नापाक होता है, तो इसका अस्ल उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता की प्राप्ति है, क्योंकि आपको अपना जिस्म और कपड़े पाक करके नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ के द्वारा बंदगी का इज़हार होता है। ख़ुद को अल्लाह के आगे झुका देना ही इबादत की अस्ल रूह है, अल्लाह के सामने पेशानी टेकना अपनी आजिज़ी और बंदगी का इज़हार है। इस हालत में इंसान को आन्तरिक और आध्यात्मिक पवित्रता के साथ-साथ ज़ाहिरी और शारीरिक तौर पर भी पाक-साफ़ होना चाहिए। पाक-साफ़ होने के लिए पानी की पाकीज़गी ज़रूरी है। यों इन तमाम गतिविधियों का अन्ततः इस रिश्ते से सम्बन्ध जा निकलता है जो अल्लाह और बन्दे के दरमियान पाया जाता है। यह शरीअत का सबसे बड़ा और सबसे पहला मौलिक उद्देश्य है।
2. जान की रक्षा
दूसरा मौलिक उद्देश्य है इंसानी जान की रक्षा। शरीअत की शब्दावली में हर इंसान ‘मासूमुद-दम’ है। उसका ख़ून सुरक्षित और मासूम है। एक इंसान की जान लेना पूरी मानवता की जान लेने के बराबर है। और एक इंसान की जान बचाना पूरी मानवता की जान बचाने के समान है। हाँ अगर स्वयं शरीअत के आदेशों ही के अनुसार उसकी हत्या को अनिवार्य क़रार दिया गया हो तो और बात है। इसकी भी केवल तीन या चार शक्लें हैं, उनके अलावा इंसानी जान लेने के औचित्य की कोई शक्ल नहीं है। या तो वह मैदाने-जंग में आपके मुक़ाबले में लड़ने के लिए आया हो, और दुश्मन हो, हमला-आवर हो। आपका क़त्ल करना चाहता हो। आपने इस्लामी राज्य की रक्षा में उस आदमी को दौराने-जंग क़त्ल कर दिया, या उसने किसी बेगुनाह को क़त्ल कर दिया था तो वह क़िसास में क़त्ल किया जा सकता है। या कुछ शर्तों के साथ इर्तिदाद (इस्लाम से फिर जाने) का अपराधी हुआ था और क़त्ल कर दिया गया। या एक और अपराध है, एक ख़ास शर्त के साथ बदकारी का अपराध किया तो उसकी सज़ा भी मौत है। इसके अलावा इंसान की जान लेने की कोई और शक्ल नहीं है। इंसान की जान सुरक्षित है। शरीअत के बहुत-से आदेश इंसानी जान की रक्षा के लिए हैं। इंसानी जान की रक्षा और जानवर की जान की रक्षा में अन्तर है। एक सुंसान जंगल में कुत्ता प्यास से मर रहा है, आपने पानी पिलाकर उसकी जान बचा दी। यह भी एक जान की रक्षा है। लेकिन इंसानी जान और कुत्ते की जान की रक्षा में बहुत अन्तर है। इंसान अल्लाह का प्रतिष्ठित प्राणी है। अल्लाह ने हर इंसान को सम्मान दिया है। हर इंसान के अन्दर अल्लाह ने वह क्षमता रखी है कि वह सम्भवत: यानी potentially अल्लाह का उत्तराधिकारी और नायब है। अत: इंसानी जान की रक्षा इज़्ज़त और प्रतिष्ठा के साथ ज़रूरी है, इंसान के सम्मान के साथ उसकी रक्षा होनी चाहिए। अगर इंसान का सम्मान शेष नहीं है तो फिर इंसानी जान की मात्र शारीरिक रक्षा काफ़ी नहीं है। अगर इंसान अपमान के साथ ज़िन्दा है तो यह इंसानी जान की रक्षा के अर्थ पर पूरा नहीं उतरता। इंसानी जान की रक्षा बतौर एक प्रतिष्ठित प्राणी के होनी चाहिए, इसलिए कि यह प्रतिष्ठा अल्लाह ने प्रदान की है। यह शरीअत का दूसरा अभीष्ट है। शरीअत के अनगिनत आदेश इंसानी जान के मान-सम्मान और इंसान के उस पद की रक्षा के लिए दिए गए हैं जिसपर अल्लाह ने इंसान को आसीन किया है।
3. बुद्धि की रक्षा
शरीअत का तीसरा उद्देश्य मानव-बुद्धि की रक्षा है। इंसान अल्लाह का उत्तराधिकारी और ख़लीफ़ा है। अल्लाह के आदेशों का पाबंद और उनका पालन करने में समर्थ है। इस कायनात में अल्लाह के बहुत-से गुणों को प्रदर्शित करनेवाला है। इन सब ज़िम्मेदारियों का पूरा करना बुद्धि पर निर्भर है। अगर इंसान बुद्धि न रखता तो उसका दर्जा जानवरों से भिन्न न होता। आख़िर जानवर भी अल्लाह की सृष्टि हैं और इंसान भी अल्लाह की सृष्टि है। जो चीज़ इंसान को अलग करती है, प्रतिष्ठित बनाती है और उसको शरई ज़िम्मेदारियों को निभाने में सक्षम करती है और जिसने इंसान को प्रतिष्ठित बनाया है वह इंसान की बुद्धि है। इसलिए बुद्धि की रक्षा शरीअत के मौलिक उद्देश्यों में से है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा ज्ञान जिससे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वह करना जायज़ नहीं है। चुनाँचे शराब पीना, मादक पदार्थों का सेवन सख़्ती से हराम क़रार दिया गया है। जितने भी ऐसे कृत्य हैं जिनसे मानव-बुद्धि प्रभावित होती हो, सम्मोहन, जादू, ये सब शरीअत में इसी लिए नाजायज़ हैं कि यह मानव-बुद्धि को प्रभावित करते हैं और सोचने-समझने की क्षमताओं को निष्क्रय कर देते हैं।
4. नस्ल की रक्षा
शरीअत का चौथा मौलिक उद्देश्य इंसान की नस्ल और परिवार की रक्षा है। इसपर आगे एक चर्चा में विस्तार से बात होगी कि नस्ल और परिवार की रक्षा को इस्लाम ने इतना महत्व क्यों दिया है और इसपर इतना ज़ोर क्यों दिया है। वे कौन-से सिद्धान्त हैं जिनसे नस्ल और परिवार बरक़रार रहें। लेकिन एक बात यहाँ बता देता हूँ। मानवजाति के स्थायित्व और निरन्तरता इसी बात पर निर्भर है कि परिवार की संस्था मौजूद और सुरक्षित हो। परिवार की संस्था मौजूद न रहे तो मानवजाति के प्रशिक्षण और स्थायित्व का सिलसिला या तो समाप्त हो जाएगा या उस नैतिक आधार पर क़ायम नहीं रहेगा जो इस्लाम क़ायम करना चाहता है।
5. माल की रक्षा
शरीअत का पाँचवाँ मौलिक उद्देश्य इंसान की सम्पत्ति और माल की रक्षा है। सम्पत्ति या माल व्यक्ति का हो या व्यक्तियों का, गिरोहों का हो या हुकूमतों का, राज्यों की मिल्कियत हो या किसी और संस्था की, इन सबकी रक्षा शरीअत के मौलिक उद्देश्यों में से है। कल मैंने वह हदीस सुनाई थी जिसमें अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने माल को नष्ट करने से मना किया है। माल किसी की मिल्कियत हो या न हो, दोनों स्थितियों में उसको नष्ट करना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि वुज़ू में दरिया का पानी भी आवश्यकता से अधिक प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। दरिया की बल खाती मौजों के उतार-चढ़ाव और प्रवाह में आपके एक-आध लोटे के बराबर पानी के प्रयोग से क्या अन्तर पड़ता है। उसका लाखों गैलन पानी तो रोज़ समुद्र में गिरता है, लेकिन वह सर्वोच्च अल्लाह गिरा रहा है, उसकी ‘मस्लहत’ (निहितार्थ) है और आप उसके ज़िम्मेदार नहीं। यह पानी समुद्र में न गिरे तो शरीअत का एक और बड़ा उद्देश्य यानी मानव-जीवन की रक्षा, वह प्रभावित हो जाए। उसकी एक अलग भौगोलिक और सृष्टिगत तत्वदर्शिता है। इससे अलग हटकर आपके लिए आदेश यह है कि आप पानी केवल उतना प्रयोग करें जितनी आपको आवश्यकता है। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की अनुमति आपको नहीं है।
शरीअत के उद्देश्यों के तीन स्तर
ये इस्लामी शरीअत के पाँच मौलिक उद्देश्य हैं। इनके अलावा भी और बहुत-सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हैं। ये चीज़ें अगरचे सीधे तौर से उन पाँच उद्देश्यों में नहीं आतीं, लेकिन उनसे आंशिक और गौण रूप से सम्बन्धित हैं। कुछ चीज़ें सीधे उन उद्देश्यों से सम्बन्धित हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। आप ग़ौर करें तो ऐसे मामलों के सैंकड़ों हज़ारों उदाहरण आपके सामने आएँगे। उदाहरण के रूप में इंसानी जान की रक्षा की ज़मानत दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के पास गर्म कपड़े नहीं हैं और वह सर्दी में खड़ा हुआ है तो जान की रक्षा के लिए उसको तुरन्त गर्म कपड़ा देना ज़रूरी है। सर्दी में गर्म और गर्मी में हल्के कपड़े देने ज़रूरी हैं। एक व्यक्ति जैकबाबाद की गर्मी में बैठा हुआ है और एक गर्म कम्बल के सिवा कोई कपड़ा उसके पास नहीं है। उसने कम्बल का तहबंद (लुंगी) बाँधा हुआ है। अगर यह कोई महिला है तो वह तो बीमार हो जाएगी। उसको ठंडा और हल्का कपड़ा देना तुरन्त आवश्यकता है। यह जान की रक्षा और उसे बाक़ी रखने की समस्या है। कोई यह नहीं कह सकता कि जान के साथ कपड़े का कोई सम्बन्ध नहीं है। इंसान का भोजन, दवा, इलाज की सुविधाएँ ये सब जान ही की रक्षा के विभिन्न दर्जे हैं। ये सुविधाएँ उपलब्ध हों तो और अच्छी सुविधाएँ दरकार होंगी। वे भी उपलब्ध हो जाएँ तो और अच्छी सुविधाएँ हैं, उनकी आवश्यकता पेश आएगी। इसकी कोई इंतिहा नहीं।
इस दृष्टिकोण से आप देखें तो जीवन के तमाम मामले शरीअत के उद्देश्यों के दायरे में आते हैं। जो भी इस दुनिया में हो रहा है, कायनात में जो कुछ भी हो रहा है उसका उन पाँच उद्देश्यों से सम्बन्ध है। इन पाँच के अलावा और कोई छठा उद्देश्य नहीं है जिससे हमारी कोई जायज़ और अक़्ली और नैतिक गतिविधि जुड़ी हो। अनैतिक गतिविधि बहुत है। फ़ुज़ूल चीज़ें बहुत हैं। लेकिन जो जायज़, उचित और सही काम हैं और जिन्हें इंसान करता है वे इन पाँच में से किसी एक की ख़ातिर करता है।
थोड़ा-सा ग़ौर करें तो स्पष्ट होगा कि इन तमाम मामलात के तीन स्तर हैं। एक स्तर वह है जिसको अपरिहार्य आवश्यकता कहते हैं। जिसको आप सख़्त ज़रूरत भी कह सकते हैं। अपरिहार्य आवश्यकता या सख़्त ज़रूरत वह है जहाँ शरीअत का कोई उद्देश्य फ़ौरी तौर पर नष्ट हो रहा हो। ये पाँच उद्देश्य, या उनमें से कोई एक उद्देश्य, या उनमें से किसी के साथ गहरा जुड़ाव रखनेवाला कोई उद्देश्य नष्ट हो रहा हो। यह अपरिहार्य आवश्यकता कहलाता है। उदाहरण के रूप में ख़ुदा-न-ख़ास्ता किसी की दुकान में आग लग गई। अगर कुछ मिनटों के अन्दर-अन्दर आग बुझाई न गई तो सारा सामान नष्ट हो जाएगा। यह तुरन्त आवश्यकता का मामला है।
इसके बाद एक दूसरा दर्जा आता है। यह तुरन्त आवश्यकता का दर्जा तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यकता का दर्जा बहरहाल है। यह आवश्यकता अगरचे तुरन्त और तीव्र नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए अरबी भाषा में ‘हाजत’ की शब्दावली प्रयुक्त होती है। शब्दावली की बात है। आप उर्दू में कोई भी शब्द इसके लिए प्रयोग कर लें। जब मैं अंग्रेज़ी में इस मामले को बयान करता हूँ तो मैं अंग्रेज़ी शब्दावली प्रयुक्त करता हूँ extreme neccesity तीव्र आवश्यकता के लिए। उसके बाद need का दर्जा है जिसके लिए अरबी शब्दावली है; हाजत। अगर आपकी कोई हाजत पूरी न हो तो आपको परेशानी होगी, मुश्किल पेश आएगी। लेकिन दोनों की जो तीव्रता है उसमें बड़ा अन्तर है। उस आग के उदाहरण को ले लें। एक बाज़ार में एक व्यक्ति की प्लास्टिक की दुकान है। एक दूसरे व्यक्ति के पास highly inflammable chemicals रखे हुए हैं। एक और के पास उदाहरणार्थ लोहे का साज़ो-सामान है। अब अगर आग लग गई तो जिसके पास लोहे का साज़ो-सामान है उसको दूसरे दुकानदारों जितना नुक़्सान नहीं होगा, कम होगा। अगर आग ज़्यादा बढ़ गई तो ज़्यादा नुक़्सान हो जाएगा वरना अक्सर चीज़ें बच जाएँगी। जिसके पास प्लास्टिक का सामान है उसका नुक़्सान बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जिसके पास फ़ौरी आग पकड़नेवाला पदार्थ है वह पलक झपकते में ही उड़ जाएगा। जिसके पास कोई और चीज़ है वह अपने हिसाब से समय लेगा। अब इन तीनों की आवश्यताओं में अन्तर है। और इस अन्तर का शरीअत में ध्यान रखा जाएगा। जब आप कोई फ़ैसला करें तो इन तीनों दर्जों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक ‘हाजत’ है, दूसरी ‘ज़रूरत’ (आवश्यकता) है, यानी तुरन्त कार्रवाई की माँग करती है।
इसके बाद तीसरा दर्जा है जिसको ‘तहसीनात’ कहते हैं। ‘तहसीन’ के शाब्दिक अर्थ हैं ख़ूबसूरत बनाना, अच्छा करना। मैं अपनी सुविधा की ख़ातिर उसका अनुवाद परफ़ेक्शन (Perfection) करता हूँ। परफ़ेक्शन वह चीज़ है कि अगर जायज़ सीमाओं में हो तो उसकी कोई सीमा नहीं। अंग्रेज़ी में कहते हैं Sky is the limit, आप जहाँ तक जाना चाहें जाएँ। अल्लाह ने आपको जितने जायज़ संसाधन दिए हैं आप वे सब संसाधन अपना लें। अल्लाह की शरीअत ने कहीं नहीं रोका कि आप किसी जायज़ मामले में अपने संसाधनों की सीमा में रहकर परफ़ेक्शन न अपनाएँ।
ये तीन दर्जे हैं, शरीअत ने जिनका पालन किया है। हर वह व्यक्ति जो किसी मामले में फ़ैसला करने का अधिकारी है, या किसी स्थिति में फ़ैसला कर रहा है, वह फ़ैसला करते समय इन तीनों दर्जों का ध्यान रखेगा। उदाहरण के रूप में आप एक घर के मालिक हैं। प्रमुख हैं। हदीस की शब्दावली में ‘रब्बुल-बैत’ हैं। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, वे सीमित हैं। सम्भव है आवश्यकताएँ ज़्यादा हों। इन ज़्यादा आवश्यताओं में आपको इन दर्जों का ध्यान रखना होगा। आपके घर में आपकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सम्भव है कोई विधवा रिश्तेदार रहती हों। कोई और ऐसी क़रीबी महिला जो आपपर निर्भर हो। किसी रिश्तेदार के बच्चे को आप गाँव से ले आए हैं कि यहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा। अब ये विभिन्न दर्जे हैं जिनकी आवश्यकताएँ भिन्न हैं। पैसे आपके पास सीमित हैं। एक बच्चा आपका ज़्यादा लाडला है। उससे आपको बड़ा प्रेम है। वह कहता है मुझे एक गाड़ी ख़रीद कर दे दें। घर में एक गाड़ी मौजूद है, लेकिन उसको अपनी अलग गाड़ी रखने का शौक़ है। उसके नज़दीक यह एक आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह है कि जो बच्चा आप गाँव से स्कूल में पढ़ाने लाए हैं उसके स्कूल की फ़ीस देनी है। पैसे वही हैं, चाहें गाड़ी ख़रीद लें, चाहें फ़ीस दे दें। तीसरी आवश्यकता यह है कि आपकी कोई ग़रीब और क़रीबी रिश्तेदार है। वह बीमार है और हस्पताल में दाख़िल है। बेचारी का बाई पास होनेवाला है और अगर तुरन्त ऑप्रेशन न हुआ तो मर जाएगी। अब शरई तौर से आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप अपनी इन शरई ज़िम्मेदारीयों को नज़रअंदाज़ करके जो आपपर लागू होती हैं अपने सीमित संसाधनों को ‘तहसीनात’ पर ख़र्च कर दें और जायज़ हाजत और तीव्र आवश्यकता को नज़रअंदाज़ कर दें। निस्सन्देह बेटा बहुत लाडला है। निस्सन्देह आपका दिल चाहता है कि इसको नई गाड़ी ख़रीद कर दें। लेकिन यह याद रखिए कि यह परफ़ेक्शनवाली बात है। तहसीनात की बात है। जिसकी फ़ीस देनी है तो वह अगर इस टर्म या वर्ष में न दी तो अगली टर्म या वर्ष उसका दाख़िला हो जाएगा। उसकी आवश्यकता गाड़ी पर वरीयता रखती है, लेकिन इतनी तीव्र नहीं कि अगर अभी फ़ीस न दी तो वह मर जाएगा या आइन्दा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन वह, जिसका ऑप्रेशन होना है अगर वह ऑप्रेशन आज न हुआ तो सम्भव है कि उसकी जान चली जाए। इसलिए आपको सबसे पहले उसपर ध्यान देना है, क्योंकि वह आवश्यकता तीव्र है। इसके बाद कुछ बचे तो आप हाजतों को पूरी करें, फ़ीस अदा करें। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फिर जहाँ जी चाहे ख़र्च कर लें और जो भी जायज़ चीज़ लेनी हो ले लें।
इस उसूल को व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामूहिक स्तर तक हर जगह चस्पाँ किया जाएगा। हर फ़ैसला करनेवाला जब मामलात का फ़ैसला करेगा, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेगा। ये तीनों इसी क्रम के साथ हैं। इनमें ‘तहसीनात’ का दर्जा अक्सर एवं अधिकतर ‘मुस्तहबात’ का होता है। शरीअत के जो ‘मुस्तहबात’ हैं वे अक्सर एवं अधिकतर तहसीनात के दायरे में आते हैं। जो सुन्नते-मुअक्कदा या वाजिबात हैं वे अक्सर ‘हाजात’ के दायरे में आते हैं। जो फ़राइज़ (कर्तव्य), अरकान (स्तम्भ) और शर्तें हैं वे तीव्र आवश्यताओं के दायरे में आते हैं। नमाज़ को आप ले लें। नमाज़ में वह कम-से-कम चीज़ जिसके बिना नमाज़ अदा नहीं होती, वे नमाज़ के अरकान (क्रियाएँ) और शर्तें हैं। उनके बिना नमाज़ नहीं होती, उनका दर्जा तो तीव्र आवश्यकता का है। इसके बाद नमाज़ की वे क्रियाएँ हैं जो सुन्नते-मुअक्कदा हैं, जिनके बिना नमाज़ हो तो जाती है, लेकिन कटी-फटी रहती है। सर्वोच्च अल्लाह के दरबार में उसको पेश करना एक दुस्साहस है। हो सकता है कि ऐसी नमाज़ पेश करने पर क़ियामत के दिन हमें शर्मिन्दगी का सामना करना पड़े, उनका दर्जा हाजात का है। इसके बाद आख़िरी दर्जा ‘मुस्तहबात’ और आदाब का है जिससे नमाज़ की शान में इज़ाफ़ा हो जाता है। इस शान में इज़ाफ़े की कोई इंतिहा नहीं। जितना इज़ाफ़ा आप करना चाहें कर सकते हैं।
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उनके भांजे उर्वा-बिन-ज़ुबैर ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की रात की नमाज़ कैसी होती थी। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने विस्तार से बयान किया कि ऐसी होती थी और ऐसी होती थी और फिर फ़रमाया कि “उसकी ख़ूबसूरती और लम्बाई का मत पूछो कि कितनी ख़ूबसूरत और कितनी लम्बी होती थी। इसलिए कि उसकी कोई इंतिहा नहीं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के बारे में आता है कि वे पूरी-पूरी रात नमाज़ में गुज़ार दिया करते थे। दो रकअत नमाज़ पढ़ने का इरादा करते थे और फिर चार, छः, आठ और पढ़ते चले जाते थे। हर सलाम के बाद में ख़याल होता था कि इस रकअत में तो अमुक ख़ामी रह गई। अमुक वस्वसा दिमाग़ में आ गया था। ध्यान इस कैफ़ियत का नहीं रहा था जो होना चाहिए। दोबारा दोहराते थे। फिर और पढ़ते। इसी दौरान में रात गुज़र जाती और फ़ज्र की अज़ान हो जाती थी। फ़ज्र की अज़ान होती थी तो रो-रोकर अल्लाह से दुआ करते कि सर्वोच्च अल्लाह के दरबार में एक नमाज़ भी ऐसी पेश नहीं कर सका जैसा कि पेश करने का ‘हक़’ है। यह सहाबा के बारे में लिखा गया है कि उनकी नमाज़ें ऐसी होती थी। यह नमाज़ों की परफ़ेक्शन है और नमाज़ों की ‘तहसीनात’ हैं। इसकी कोई इंतिहा नहीं। आदमी जिस दर्जे तक पहुँचाना चाहे पहुँचा सकता है।
इसी तरह शरीअत के तमाम उद्देश्य, तमाम आदेश और हर चीज़ में एक दर्जा कमाल (परिपूर्णता) या पूर्ति का होगा जिसके अनगिनत मज़ीद दर्जे हो सकते हैं। इसलिए कि पूर्ति और पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। हर अच्छी और लाभकारी चीज़ में शरीअत की सीमाओं के अन्दर ‘कमाल’ की प्राप्ति प्रिय है। कमाल से निचला दर्जा हाजात का है। यह वह दर्जा है कि अगर यह प्रभावित हो जाए तो इससे इस उद्देश्य या काम में नुमायाँ त्रुटि पैदा हो जाती है। सबसे निचला दर्जा अपरिहार्य आवश्यकता का है। जिससे कम में वह इबादत या वह उद्देश्य या अमल अपने मौलिक गुणों, बल्कि अपनी मौलिक वास्तविकता और स्वरूप से वंचित हो जाता है। आवश्यकता का दर्जा गोया bare minimum का है जिससे नीचे का दर्जा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कि इससे कम में इस चीज़ की वास्तविकता ही शेष नहीं रहती है। उदाहरणार्थ घर है। घर के कम-से-कम शर्तें यह हैं कि चारदीवारी और छत हो। फ़र्श कच्चा हो, रौशनी-पानी न हो, और कुछ न हो लेकिन कम-से-कम एक छत और चार-दीवारी तो हो। छत और चार-दीवारी न हो तो इससे कम को घर कोई नहीं कहता। यह गोया अपरिहार्य आवश्यताओं की बात है। इसके बाद का दर्जा यह है कि उसमें खिड़कियाँ हों, शीशे भी लगे हों, ताकि रात ठंडी हवा न आए। दरवाज़ा भी लगा होता कि कोई बिना अनुमति घुसने न पाए। यह हाजात हैं जिनके बिना इंसान के लिए उस घर में रहना मुश्किल होगा। और तीसरा दर्जा यह है कि आपको राहत और आराम का जो भी सामान उपलब्ध हो, आप उसको जायज़ सीमाओं के अन्दर रहते हुए अपना सकते हैं। यह तहसीनात का दर्जा है।
ये शरीअत के मौलिक उद्देश्य हैं। क़ुरआन और सुन्नत के आधार पर सर्वोच्च अल्लाह ने प्रतिष्ठित क़ुफ़हा को जो समझ प्रदान की, जो इज्तिहादात उन्होंने संकलित किए, और जो फ़िक़्ह उन्होंने संकलित की, उनमें से हर-हर आदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। उनमें से कोई चीज़ या तो सीधे स्वयं ही उद्देश्य है। या वह तहसीनात के दर्जे में है, या वह हाजात के दर्जे में और या फिर उसका दर्जा ज़रूरतों का है।
इस बात का निर्धारण करने में कि क्या चीज़ हाजात में से है और क्या तहसीनात में शामिल है, कभी-कभी मुश्किल पेश आती है। यह निर्धारण करना आसान काम नहीं होता। ख़ालिस तौर पर इन मामलों के बारे में जो बज़ाहिर जायज़ कामों के दायरा में आते हों। यह तय करना कि ये चूँकि तहसीनात की हैसियत रखते हैं इसलिए इनको अपनाने में किसी ख़ास चिन्तन-मनन की आवश्यकता नहीं। इस तरह के मामलों में एक मौलिक सिद्धान्त सामने रखना चाहिए। यह इस्लाम में शरीअत की तत्वदर्शिता का मौलिक सिद्धान्त है। जब किसी चीज़ के अच्छा या बुरा होने का आपको फ़ैसला करना हो तो यह उसूल बहुत मार्गदर्शन करता है। इबादात में तो यह फ़ैसला करना बहुत आसान है। जहाँ शरीअत के स्पष्ट वाजिबात और मुहर्रमात का मामला हो, वहाँ भी आसान है। लेकिन बहुत-से मामलात ऐसे हैं जहाँ शरीअत के वाजिबात और इबादात से वास्ता नहीं पड़ता। इन मामलात में शरीअत ने आपको आज़ाद छोड़ा है और आप स्वयं फ़ैसला कर सकते हैं। उनमें कुछ मामलात ऐसे पेश आ जाते हैं जिनमें इंसान को मुश्किल पेश आती है कि वह क्या फ़ैसला करे। किन चीज़ों को हाजात क़रार दे, किन को आवश्यकताएँ ठहराए और किन को तहसीनात क़रार दे। इसका एक सिद्धान्त याद रखें। सिद्धान्त यह है कि अन्ततः इस कार्य का क्या परिणाम निकलेगा। इमाम शातबी ने लिखा है कि “शरीअत में इस बात को सामने रखा जाता है कि अन्ततः यानी काम का अंजाम क्या होगा।” उदाहरणार्थ एक जायज़ काम है। शरीअत ने आपको उसके करने या न करने का आदेश नहीं दिया। दोनों स्थितियाँ आपके लिए खुली छोड़ दी हैं। उसको न मुस्तहब क़रार दिया है न मकरूह। लेकिन जब उसपर अमल करने या न करने का फ़ैसला करने लगें, तो आप यह ज़रूर ग़ौर करें कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। उसके परिणामस्वरूप जो फल सामने आएँगे वे सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर इस कार्य के परिणाम सकारात्मक हों तो वह काम करें और अगर नकारात्मक हो तो न करें। यह शरीअत की तत्वदर्शिता है जो शरीअत ने सामने
रखी है।
शरीअत की तत्वदर्शिता के महत्वपूर्ण सिद्धान्त
शरीअत की इस तत्वदर्शिता के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं जो पवित्र क़ुरआन ने दिए हैं। जो हर फ़क़ीह को और हर विद्वान को सामने रखने चाहिएँ।
1. युस्र और आसानी
सबसे पहला सिद्धान्त है ‘युस्र’ यानी आसानी। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है— “सर्वोच्च अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी (युस्र) चाहता है मुश्किल नहीं चाहता।” (क़ुरआन, 2:185) युस्र से मुराद वह आसानी है जो शरीअत के किसी आदेश को अंजाम देते हुए या शरीअत द्वारा हराम ठहारई हुई चीज़ों से बचते हुए आपके लिए अपनाना सम्भव हो। जहाँ शरीअत के आदेशों पर अमल करते हुए आपकी दरकार आसानी सम्भव न हो वहाँ ‘युस्र’ के नाम पर शरीअत के आदेश को नहीं छोड़ा जा सकता। उदाहरणार्थ यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगस्त का महीना है और शदीद गर्मी और जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल है। शरीअत का आदेश है कि आसानी पैदा करो, अत: मैं रोज़ा न रखूँ और ठंडे कमरे में बैठकर शरबत पियूँ। ‘युस्र’ का यह मतलब नहीं है। ‘युस्र’ का मतलब यह है कि गर्मी में रोज़ा रखते हुए कोई आसानी अगर उपलब्ध कर सकते हो तो ज़रूर करो। अगर आपकी यह संस्था इस कमरे में एयर कंडीशनर लगवा दे कि गर्मी का मौसम है इससे रोज़ा रखने में आसानी होगी, तो यह ‘युस्र’ है। यानी वे आसानियाँ जो शरीअत के किसी आदेश के पालन, या शरीअत द्वारा हराम ठहारई चीज़ों से बचने में आसानी के लिए पैदा की जाएँ वे ‘युस्र’ के अर्थ में आती हैं। या कोई जायज़ काम इसलिए किया जाए कि इससे शरीअत के अमुक आदेश का पालन आसान हो जाए। जीवन और जीवन की समस्याएँ आसान हो जाएँ। यह चीज़ ‘युस्र’ कहलाती है। सर्वोच्च अल्लाह की शरीअत में इसी अर्थ में ‘युस्र’ है, ‘उस्र’ (तंगी) नहीं।
2. रफ़अ हरज
दूसरी चीज़ है ‘रफ़अ हरज’ यानी तंगी और परेशानी को दूर करना। क़ुरआन में कहा गया है— “सर्वोच्च अल्लाह ने दीन में कोई तंगी नहीं रखी।” (क़ुरआन, 22:78) इससे मुराद यह है कि शरीअत के आदेशों का पालन करने के अगर दो तरीक़े हों। एक तरीक़ा आसान हो और दूसरा मुश्किल हो, तो सर्वोच्च अल्लाह ने मुश्किल रास्ता अपनाने का आदेश नहीं दिया, अत: जहाँ भी मुश्किल रास्ता नज़र आए, वहाँ ठहरो, सोचो, अगर इस मुश्किल रास्ते से बचने का कोई आसान रास्ता है, जिससे शरीअत के आदेश का पालन भी हो जाए और मुश्किल से भी बचा जाए तो मुश्किल से बचोगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जो फ़िक़्ह के छात्रों को याद रखना चाहिए। बहुत-से लोग इस ग़लत-फ़हमी में मुब्तला रहते हैं कि ख़ाह-मख़ाह मुश्किलों को दावत देना और परेशानियों को अकारण अपना लेना दीनदारी का तक़ाज़ा या कम-से-कम निशानी ज़रूर है। उदाहरणार्थ आपपर हज फ़र्ज़ है। अल्लाह ने आपको संसाधन भी दिए हैं। अब हज करने का एक तरीक़ा तो यह हो सकता है कि आप कपड़ों के एक दो जोड़े और चनों का थैला साथ ले लें और पैदल चल पढ़ें। अतीत में लोग बड़ी संख्या में पैदल हज के लिए जाया करते थे। यह एक तरीक़ा है, शरीअत में इसकी मनाही नहीं। अगर आपके पास सफ़र के जायज़ संसाधन मौजूद न हों और आप में हिम्मत हो कि पैदल मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र कर सकें तो ज़रूर करें, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको संसाधन दिए हैं तो फिर बेहतर तरीक़ा यह है कि आप फ़र्स्ट क्लास टिकट लेकर जहाज़ में बैठ जाएँ, होटल में बुकिंग करवा लें। जाएँ और हज करके वापस आ जाएँ। अगर आपके पास दोनों तरह के संसाधन हैं तो आपके लिए पहला रास्ता अपनाना दुरुस्त नहीं। शरीअत में पहला रास्ता मकरूह होगा। नापसंदीदा रास्ता होगा कि संसाधन होते हुए आप पैदल सफ़र का रास्ता अपनाएँ।
मैंने कुछ लोगों को देखा है जो यह कहते हैं कि जनाब पैदल हज करने जाना बड़ा अफ़ज़ल है। इसलिए उन्होंने पैदल हज किया और दो-दो वर्ष सफ़र में गुज़ार दिए। मैंने पूछा कि आपने पैदल हज क्यों किया? क्या पैसे नहीं थे? जवाब मिला कि नहीं पैसा तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत था। लेकिन बस ज़्यादा सवाब के लिए। मैंने कहा कि सर्वोच्च अल्लाह को ऐसी फ़ुज़ूल हरकत की कोई आवश्यकता नहीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी पैदल हज नहीं किया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने संसाधन की मौजूदगी में कभी पैदल हज नहीं किए। ताबिईन ने संसाधन होते हुए कभी पैदल हज नहीं किया। अगर संसाधन होते थे तो वे ज़रूर प्रयुक्त करते थे। संसाधन को बचाकर घर में रखें और अल्लाह पर एहसान करने के लिए पैदल हज करें तो यह शरीअत के स्वभाव और शिक्षा के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। यह चीज़ शरई तौर से विश्वसनीय नहीं है, न शरई तौर से इसको पसंदीदा क़रार दिया गया है।
3. दफ़अ मशक़्क़त
तीसरी चीज़ है ‘दफ़अ मशक़्क़त’ यानी मशक़्क़त और परेशानी को दूर करना। बज़ाहिर यह ‘रफ़अ हरज’ ही का एक पहलू मालूम होता है, लेकिन ज़रा ग़ौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह ‘रफ़अ हरज’ से किसी हद तक भिन्न चीज़ है। मशक़्क़त से मुराद यहाँ वह मुश्किल या परेशानी है जो अचानक पेश आ जाए। किसी वक़्ती स्थिति में पैदा हो जाए। उदाहरणार्थ इंसान बीमार हो जाता है। सफ़र पर जाता है तो बहुत-से ऐसे उपाय अपना नहीं सकता जो घर में अपना सकता है। ये वे चीज़ें हैं जो अस्थायी रूप से मुश्किल पैदा करती हैं। जब अस्थायी मुश्किल पैदा होती है तो अस्थायी आसानी भी पैदा हो जाती है। उदाहरणार्थ ‘अज़ीमत’ (दृढ़ संकल्प) की बजाय ‘रुख़स्त’ (छूट) को अपना सकता है। सफ़र में इंसान अल्लाह की दी हुई रुख़स्त से फ़ायदा न उठाए और ग़ैर-ज़रूरी तौर पर मुश्किलें बर्दाश्त करे, यह चीज़ शरीअत के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज्जतुल-विदा के लिए जा रहे थे। आपको पता चला कि कुछ सहाबा ने रोज़ा रखा हुआ है। यह शदीद गर्मी के मौसम में मदीना मुनव्वरा से मक्का का सफ़र था। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के बारे में पता चला कि गर्मी का यह सारा सफ़र उन्होंने रोज़े की हालत में किया है और अब भूख, गर्मी और प्यास से निढाल हो गए। एक जगह आपने देखा कि लोग एक ख़ेमे के बाहर जमा हैं। पूछा तो बताया गया कि अमुक साहब ने रोज़ा रखा हुआ है और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गए हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है।” यानी ऐसी स्थिति में जहाँ सफ़र की तंगी और मुश्किलों की वजह से आसानी से रोज़ा न रखा जा सकता हो। अलबत्ता अगर ऐसी स्थिति न हो और आपको अगर ऐसी कोई समस्या पेश न आए और आपको अपनी सेहत पर भरोसा हो तो सफ़र में भी रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी परेशानी को बर्दाश्त करना और रोज़े पर आग्रह करना गोया सर्वोच्च अल्लाह की दी हुई रुख़सत की नाक़द्री है। ऐसे परिस्थितियों में रुख़स्त को प्रयुक्त न करने का मतलब गोया यह दावा करना है कि अल्लाह ने तो अनुमति दी है, लेकिन चूँकि मैं बहुत बहादुर भी हूँ और परहेज़गार भी दूसरों से ज़्यादा हूँ इसलिए रोज़ा रख सकता हूँ। अत: ऐसा कहना या ऐसा तर्ज़े-अमल अपनाना, अल्लाह की पनाह, उसकी नेमत का इनकार है। इसलिए जहाँ परेशानी की सम्भावना हो वहाँ रुख़स्त से फ़ायदा उठाना चाहिए।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़त्हे-मक्का के लिए जा रहे थे। रमज़ानुल-मुबारक का महीना था। कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का रोज़ा था। अब जिहाद के लिए जा रहे थे। हो सकता है वहाँ जंग का सामना करना पड़े। थके-माँदे और भूख-प्यास की हालत में वहाँ पहुँचेंगे तो क्या जिहाद करेंगे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस स्थिति का एहसास किया और मौखिक आदेश देने के बजाय अपने व्यवहार से न केवल इस सम्भावित परेशानी को दूर किया, बल्कि हमेशा के लिए सुन्नत भी क़ायम कर दी। इस मौक़े पर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऊँट पर सवार थे। आपने तमाम सहाबा के सामने एक सहाबी से कहा कि ज़रा ठंडा दूध लेकर आओ। दूध पेश किया गया तो आपने सबके सामने दूध पिया। यह दिखाने के लिए कि मैंने रोज़ा नहीं रखा। यह वह चीज़ है जिसको ‘दफ़अ मशक़्क़त’ कहते हैं। यानी अगर वक़्ती तौर पर कोई मुश्किल पेश आ गई है तो उसको दूर कर दिया जाए।
4. लोगों की ‘मस्लहत’ का ख़याल
चौथी चीज़ है लोगों की ‘मस्लहत’ का ध्यान रखना। लोगों की इस ‘मस्लहत’ का ध्यान रखना जिसको शरीअत ने विश्वसनीय समझा हो। शरीअत में वे मस्लहतें महत्वपूर्ण हैं जिनका सम्बन्ध उन पाँच उद्देश्यों से हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की जायज़ मस्लहतों को पूरा करती हों। ऐसी हर ‘मस्लहत’ का ध्यान रखा जाए और उसको अकारण नज़रअंदाज़ न किया जाए। जिस हद तक आप ध्यान रख सकते हैं उस हद तक ध्यान रखना चाहिए। लोगों से यह आशा रखना कि उदाहरणार्थ इस्लामाबाद की सब महिलाएँ अपने घरों और पतियों को छोड़कर एक-एक वर्ष के लिए ख़ाली हो जाएँ और दीन की शिक्षा के लिए आ जाएँ। ऐसा करने से उनके बहुत-से जायज़ और ज़रूरी काम रुक जाएँगे। इन ज़रूरी कामों को छोड़कर कोई नहीं आएगा। यह सम्भव नहीं है। अब अगर आप फ़तवा जड़ दें कि जनाब यह तो सब बेदीन लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की समस्याएँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं। उनकी मुश्किलों का ध्यान रखें। उनको देखें कि किस वजह से उनके लिए आना मुश्किल है, किस वजह से वे नहीं आ सकते। उनकी मशक़्क़त और ‘मस्लहत’ का ध्यान करते हुए उनके लिए दीन की शिक्षा का कोई प्रोग्राम बनाएँ। यह दुरुस्त है कि कुछ लोग एक वर्ष के या कई वर्षों के लिए आ सकते हैं, लेकिन बहुत-से लोग ऐसे हैं जो कुछ महीनों, बल्कि शायद कुछ हफ़्तों के लिए भी नहीं आ सकते। पवित्र क़ुरआन ने आदेश दिया है कि हर गिरोह में से कुछ लोग आएँ, और दीन सीखकर वापस चले जाएँ। पवित्र क़ुरआन ने इस सम्भावना को सामने रखा है।
5. तदरीज
पाँचवीं चीज़ जो शरीअत ने सामने रखी है वह ‘तदरीज’ है। तदरीज का अर्थ यह है कि शरीअत के आदेशों पर आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा करके क्रमशः अमल कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति दीन सीखने के लिए आपके पास आया है तो आज ही सारे-का-सारा दीन उसपर न लाद दें। उसको क्रमशः दीन की तरफ़ लाएँ। पहले मौलिक सिद्धान्त उसको बताएँ, फिर जब वह और क़रीब आ जाए और ईमान ज़्यादा पक्का हो जाए तो उसके नैतिक आचरण पर ध्यान दें। जब नैतिक आचरण दुरुस्त हो जाए तो फिर एक-एककर सारे आदेश उसको बताएँ। और फिर उसको जितना शौक़ पैदा होता जाएगा उतना ही जल्दी वह सारे-का-सारा दीन सीख लेगा। यह पवित्र क़ुरआन की तरीक़ा भी है, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का तरीक़ा भी यही था और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का भी यही तरीक़ा था। तदरीज और लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता दीन के रास्ते पर लाना यह अल्लाह की शरीअत की मौलिक कार्य प्रणाली और अल्लाह की सुन्नत है।
6. अद्ल
छठी चीज़ अद्ल अर्थात् न्याय है। लोगों के लिए नियम-क़ानून बनाने या कोई व्यवस्था बनाने में अद्ल और इंसाफ़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यह शरीअत की तत्वदर्शिता का एक और आधार है। आप कोई संस्था क़ायम करना चाहें और उसमें छात्रों के लिए नियम-क़ानून बनाएँ तो अद्ल का ध्यान रखें। अपने कर्मचारियों और बच्चों और घरवालों से मामला करते समय अद्ल और इंसाफ़ का ध्यान रखें। शरीअत का पालन करने में अद्ल का ख़याल रखना अत्यन्त ज़रूरी है। अद्ल की अपेक्षा विशुद्ध निजी मामलों से लेकर पारिवारिक, सामूहिक, आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी अद्ल की इस्लामी अपेक्षाओं की पैरवी शरीअत की तत्वदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।
एक सहाबी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में हाज़िर हुए। कहने लगे कि “ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपनी सम्पत्ति का इतना हिस्सा अपने अमुक बेटे को देना चाहता हूँ, आप गवाह रहें।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। उन्होंने संख्या बताई। आपने पूछा क्या शेष बच्चों को भी इतना ही हिस्सा दे रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं सबको तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चूँकि यह एक बच्चा मुझको बहुत प्रिय है इसलिए केवल इसी को दे रहा हूँ। आपने फ़रमाया कि “मैं ज़ुल्म का गवाह नहीं बनना चाहता।” यानी यह बच्चों के साथ अद्ल (न्याय) के ख़िलाफ़ है कि आप एक बच्चे को ग़ैर-ज़रूरी प्राथमिकता दें और शेष को उपेक्षित कर दें।
7. मुसावात और बराबरी
सातवीं और आख़िरी चीज़ यह है कि आप मुसावात अर्थात् समानता क़ायम रखें। इनसानों के बीच समानता इस्लामी शरीअत के मौलिक और मूल आदेशों में से है। इस्लाम की समानता की धारणा ही का करिश्मा था कि कुछ दशकों के अन्दर-अन्दर इस्लाम की किरणें तीनों महाद्वीपों तक जा पहुँचीं। जब तक मुसलमान मानव समानता के इस्लामी सिद्धान्त पर कार्यरत रहे इस्लाम का पर्चम ऊँचा रहा और मुसलमानों का सितारा चमकता रहा, लेकिन जब मुसलमानों ने क्षेत्रीय, भाषागत और जातिगत भेदभावों से प्रभावित होकर मानवीय समानता की धारणा को भुलाना शुरू कर दिया तो उनके वर्चस्व का दौर भी सिमटना शुरू हो गया। अफ़सोस यह है कि आज मुसलमान भी समानता की इस्लामी धारणा को पूरे तौर पर भुला चुके हैं और पूरब एवं पश्चिम से आयातित क्षेत्रीय और जातीय तथा भाषाई भेदभावों की ग़ैर-इस्लामी धारणा पर कार्यरत हैं।
शरीअत की तत्वदर्शिता में एक और महत्वपूर्ण चीज़ भी सामने रखनी चाहिए जो शरीअत के आदेशों में एक मौलिक भूमिका निभाती है। शरीअत की शिक्षा के जितने भी विभाग हैं उनके तीन प्रकार तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। जिसमें एक अक़ाइद (धारणाएँ), दूसरा नैतिक आचरण और तज़किया (शुद्धीकरण) और तीसरा फ़िक़ही (धर्मशास्त्रीय) मामले हैं। फिर फ़िक़ही मामलों में मैंने आठ विभिन्न अध्याय बताए थे। यह विभाजन तो आपके और हमारे समझने के लिए था।
एक विभाजन और है जो शरीअत के स्वभाव को बयान करने के लिए है कि शरीअत का स्वभाव किस मामले में क्या है। इस दृष्टि से कुछ मैदान या कुछ समस्याएँ और मामले तो वे हैं कि जिनमें शरीअत का रवैया बिलकुल स्पष्ट, कड़ा और strict होना है। इन मामलों में शरीअत अत्यन्त सख्त है। इन मामलों में जिस चीज़ का शरीअत ने जितना आदेश दिया है बस उतना ही करना है, इसमें कोई कमी-बेशी करने की अनुमति नहीं है। इन मामलों में शरीअत द्वारा निर्धारित सीमाओं से न एक क़दम आगे जाना जायज़ है न एक क़दम पीछे रहना स्वीकार्य है। इन दोनों की अनुमति नहीं है। जिस हद तक अमल करने को कहा गया है वहाँ तक करना है। जहाँ ज़्यादा करने की अनुमति दी है वहाँ इन्हीं सीमाओं के अन्दर रहकर ज़्यादा अमल कर सकते हैं जो बताई गईं हैं। जहाँ कमी करने की अनुमति है वहाँ भी केवल उसी हद तक कमी कर सकते हैं जिस हद तक कमी करने की अनुमति दी गई है। जहाँ कमी-ज़्यादती की अनुमति नहीं, वहाँ कमी-ज़्यादती बिलकुल नहीं की जा सकती। ये वे मामले हैं जहाँ अपनी बुद्धि से कोई नई बात अपनाई नहीं जा सकती, बल्कि निर्धारित निर्देश ही का सौ प्रतिशत पालन करना चाहिए। ये मामले अक़ीदों (धार्मिक अवधारणाओं) और इबादतों के हैं।
अक़ीदों और इबादतों में इंसान अपनी राय, बुद्धि और अपने अनुमान से न कमी कर सकता है न ज़्यादती कर सकता है। कोई कहे कि जनाब मेरा दिल तो अल्लाह के हुज़ूर झुकने को बहुत चाहता है मेरी तो एक रकअत में एक रुकू से तसल्ली नहीं होती में तो चार-बार रुकू किया करूँगा। ऐसी नमाज़ बातिल और ग़लत होगी और जायज़ नहीं होगी। किसी का जी चाहे कि मेरा तो सजदा करने को बहुत दिल चाहता है, मैं एक रकअत में दो की बजाय दस सजदे किया करूँगा। ऐसी नमाज़ भी बातिल है। चाहे चार रुकू और दस सजदे करनेवाला बन्दगी के कितने ही निष्ठाभाव से यह काम करना चाहता हो, चाहे उसके दिल में अल्लाह से प्रेम की कैसी ही सख़्त भावना हो, नमाज़ उसकी रद्द ही होगी। इबादतों में बढ़ोतरी की तरह कमी भी ग़लत है। उदाहरणार्थ किसी की बुद्धि में आया कि जी एक बार झुकना और एक बार सजदा करना काफ़ी है। दो सजदों की क्या आवश्यकता है। शैतान कुछ भी समझा सकता है। ऐसी स्थिति में भी नमाज़ बातिल (ग़लत) हो जाएगी और स्वीकार्य नहीं होगी।
सारांश यह कि अक़ीदों और इबादतों में कोई कमी-बेशी जायज़ नहीं। सिवाय यह कि शरीअत ही ने अनुमति दी हो। उदाहरणार्थ नफ़्ल इबादत की अनुमति दी है तो जितनी मर्ज़ी हो पढ़ लें। लेकिन नवाफ़िल भी उस तरीक़े से पढ़ने होंगे जिस तरीक़े से शरीअत ने शिक्षा दी है। उसके अलावा किसी और तरीक़े से नवाफ़िल भी जायज़ नहीं होंगे। अगर कोई कहे कि जी नफ़्ल में क्या है, मैं तो एक रकअत में दस सजदे करूँगा। नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। एक रकअत में रुकू एक ही होगा और सजदे दो ही होंगे। जिस तरह शरीअत ने कहा है उसी तरह करना होगा। हाँ रकअतों की संख्या में आप आज़ाद हैं, चार पढ़ें, दस पढ़ें, जितना मर्ज़ी नमाज़ को लम्बी कर लें, इसकी आपको अनुमति है। इससे ज़्यादा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यहाँ शरीअत का मामला बहुत सख़्त है।
इसके बाद मामलात की बात है। इसमें शरीअत ने थोड़ी सी नरमी रखी है। शरीअत का रवैया यहाँ तुलनात्मक रूप से lenient (उदारवादी) है। मामलात के बारे में शरीअत ने यह किया है कि जो चीज़ें नाजायज़ हैं वे बता दी हैं। उनकी सीमाबन्दी कर दी है कि अमुक-अमुक चीज़ें हराम हैं। उदाहरणार्थ ब्याज हराम है, ग़रर (धोखा) हराम है, क़िमार (जूआ) हराम है, ततफ़ीफ़ (तौल में डंडी मारना) हराम है। मामलों पर विस्तृत चर्चा एक दिन अलग से होगी। पवित्र क़ुरआन और सुन्नत ने मुहर्रमात (निषिद्ध ठहारई हुई चीज़ों) की सूची दी है। और जो चीज़ें अनिवार्य हैं और संख्या में कम हैं उनका विवरण दे दिया है। इन मुहर्रमात से बचते हुए और उन अनिवार्य चीज़ों का पालन करते हुए आप मामलों में जो करना चाहें वह करें, जो कार्य प्रणाली आपको पसंद हो वह अपनाएँ। जिस तरह का मामला आप करना चाहें, आपके अधिकार में है। कोई कारोबारी या व्यापारिक मामला नाजायज़ नहीं, अगर वह शरीअत के मुहर्रमात से बचकर हो, और जो कुछ आम वाजिबात और फ़राइज़ (अनिवार्य आदेश) हैं उनके अनुसार हो। यानी कुछ निर्धारित हराम की हुई चीज़ों के अलावा सब चीज़ें आपके लिए जायज़ हैं।
जिन मामलात में शरीअत का रवैया बहुत ज़्यादा खुला और liberal है वह ‘आदात’ का मामला है। ‘आदात’ यानी विभिन्न क्षेत्रों के रीति-रिवाज, लोगों की रस्में और तौर-तरीक़े, और विभिन्न संस्कृतियों की निशानियाँ, सामाजिक रहन-सहन में लोगों का विभिन्न रवैया और स्वभाव, ये चीज़ें जो हर इलाक़े और क़ौम में विभिन्न हो सकती हैं, ‘आदात’ कहलाती हैं। ‘आदात’ में हर चीज़ जायज़ है। बशर्तिके वह शरीअत की आम सीमाओं के अन्दर हो। उससे किसी हराम चीज़ का अपराध न होता हो और किसी फ़र्ज़ या वाजिब को छोड़ना लाज़िम न होता हो। इस आम शर्त के अलावा ‘आदात’ में कोई प्रतिबन्ध नहीं। हर क़ौम का लिबास भिन्न होगा। खाने-पीने का तरीक़ा भिन्न होगा। कोई क़ौम चावल पसंद करती होगी कोई गेहूँ, कोई क़ौम इन दोनों के अलावा कोई और चीज़ खाती होगी। शरीअत में ये सब ‘आदात’ जायज़ और स्वीकार्य हैं। शरीअत में इस मामले में कोई सख़्ती या प्रतिबन्ध नहीं। शरीअत ने किसी क़ौम की ‘आदात’ यहाँ तक कि क़ुरैश और हिजाज़ के लोगों की ‘आदात’ और परम्पराएँ भी दूसरों के लिए ज़रूरी क़रार नहीं दी हैं। इस पहलू को बहुत-से इस्लाम के प्रचारक नज़रअंदाज़ कर देते हैं। बहुत-से जोशीले लेकिन कम समझ और कम ज्ञान रखनेवाले इस्लाम के प्रचारक अपने क्षेत्र और अपने वतन की ‘आदात’ और रिवाजों को शरीअत के बराबर क़रार देकर दूसरों से, विशेषकर नव-मुस्लिमों से उनके पालन की माँग करते हैं जो न केवल ग़लत है, बल्कि इस्लाम की ओर आह्वान की तत्वदर्शिता के भी ख़िलाफ़ है।
मैंने आज से पंद्रह-सोलह वर्ष पहले एक अजीब-ग़रीब क़ौम देखी। मुझे फ़िजी जाने का मौक़ा मिला। यह अत्यन्त पूरब में इंटरनेशनल डेट लाइन पर बहुत-सारे द्वीपों का संग्रह है। वहाँ कुछ द्वीपों में एक क़ौम रहती है जो बिलकुल आरम्भिक और primitive अंदाज़ में रहती है पुरुष और महिलाएँ सब अर्धनग्न रहते हैं। एक मामूली सा जांघिया बाँधते हैं उसके अलावा कोई लिबास नहीं पहनते। न उनका घर होता है, न कारोबार है, न शिक्षा का कोई सिलसिला है। वृक्षों पर घोंसलों की तरह झुग्गियाँ और झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। उनकी ख़ुराक यह है कि वे बाहर निकलते हैं और समुद्र में केकड़े पकड़ते हैं। उसका पेट फाड़कर जो कुछ निकलता है उसको कच्चा खा जाते हैं। मैंने स्वयं यह मंज़र देखा कि बच्चे जवान सब डंडा हाथ में लिए केकड़े की प्रतीक्षा में खड़े होते हैं और ज्यों ही कोई केकड़ा नज़र आ जाए तो पकड़कर उसकी कमर तोड़कर जो कुछ निकले उसको खा लेते हैं। अगर केकड़ा न मिले तो एक जंगली फल वहाँ बहुत होता है, जो हमारे यहाँ के केले और शकरक़ंद से मिलता-जुलता है, उसको खा लेते हैं। उसका मज़ा अजीब-सा होता है, लेकिन लोगों ने बताया कि बहुत ताक़तवर और पौष्टिकता से भरपूर होता है। मैंने चखकर देखा, लेकिन न वह स्वादिष्ट था और न बद-मज़ा, इसलिए पसंद नहीं आया। ये दो चीज़ें उनकी ख़ुराक हैं। इस क्षेत्र की बड़ी आबादी ने जीवन में कभी भी गेहूँ या चावल या गोश्त नहीं खाया। ये लोग हज़ारों वर्ष से वहाँ रहते हैं। लोगों ने उनसे कहा कि भाई शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने पूछा, शिक्षा? उससे क्या होगा। बताया गया कि अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, उन्होंने कहा उससे क्या होगा? जवाब दिया गया कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। उन्होंने पूछा उससे क्या होगा? बताया गया कि अच्छा खाना खाओगे। उन्होंने कहा कि वह तो हम अब भी खा रहे हैं।
अब अगर यह क़ौम इस्लाम स्वीकार कर ले और आप उनसे कहें कि केकड़ा मत खाओ, तो ऐसी माँग करना न केवल शरीअत की तत्वदर्शिता के ख़िलाफ़ होगा, बल्कि इस्लाम की ओर आह्वान की तत्वदर्शिता के भी विरुद्ध होगा। चूँकि इमाम शाफ़िई (रह॰) और इमाम मालिक (रह॰) के नज़दीक केकड़ा खाना जायज़ है इसलिए मैं कम-से-कम तुरन्त इस चीज़ पर आपत्ति नहीं करूँगा। इस तरह वह फल खाना भी बिलकुल जायज़ है जिसको वे खाते हैं। अगर उनके इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी मुझे उनके दरमियान कुछ अरसा रहने का मौक़ा मिले तो फिर मैं उनकी महिलाओं से कुछ समय के बाद कहूँगा कि ज़रा ज़्यादा लिबास पहना करें। और कम-से-कम सीना और टांगें पूरी तरह ढाक लें। उसके अलावा मैं उन्हें कोई और काम करने को नहीं कहूँगा। इसलिए कि यह तो ‘आदात’ का मामला है और शरीअत ने ‘आदात’ के मामले में लोगों को आज़ाद रखा है। अगर एक पूरी क़ौम इस्लाम स्वीकार कर ले और उनके यहाँ कोई ख़ास रिवाज हो जिसके वे सब आदी हों और वे उसके अनुसार रहना चाहें, तो शरई तौर से कोई चीज़ रुकावट नहीं है। सिवाए इसके कि लिबास में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करके अपने जिस्म को थोड़ा-सा और ढाँक लें। बाक़ी जंगल में पेड़ों पर ही रहना चाहें तो वहाँ रहें, शहर में बसना चाहें तो शहर में बसें। केले की तरह का फल खाना चाहें तो वह खाएँ, यह उनका फ़ैसला है उनको करने दें। अगर वह डंडा मारकर केकड़ा खाते हैं, मैं कहूँगा कि इमाम मालिक (रह॰) के नज़दीक समुद्र की तमाम चीज़ें खाना जायज़ हैं और यह शरई तौर से हराम नहीं है। वह शौक़ से अपना पूरा जीवन इस तरह गुज़ारें। रोज़ा रखें और नमाज़ पढ़ते रहें, ज़कात और हज तो ज़ाहिर है उनपर फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख़याल में उनके अच्छा मुसलमान बनने में कोई रुकावट नहीं है।
यह मामला ‘आदात’ का है। शरीअत ने ‘आदात’ में लोगों को आज़ाद छोड़ा है। यह बात मैंने विस्तार से इसलिए बयान की कि हममें से बहुत-से लोगों का यह अंदाज़ इस मामले में ग़ैर-ज़रूरी सख़्ती का होना है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत और कई दूसरे क्षेत्रों के मुसलमानों का लगभग यह अंदाज़ होता है कि उन्होंने जो कुछ अपने इलाक़े में देखा होता है उसी को दीन समझते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती अपने क्षेत्र की ‘आदात’ पर जीवन गुज़ारने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अगर कोई भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के हाथ पर इस्लाम स्वीकार करे तो उसको ज़बरदस्ती शलवार क़मीज़, सद्री और क़राक़ुली (एक विशेष प्रकार की टोपी) पहनाएँगे। हालाँकि इन चीज़ों का इस्लाम में कोई आदेश नहीं है। अगर आपको उसके कपड़ों पर हिजाब की दृष्टि से आपत्ति है या कोई पुरुष रेशम पहने, या औरतें पुरुषों जैसे और पुरुष स्त्रियों जैसे कपड़े पहनते हों तो इसको तो निस्सन्देह दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन उनके अलावा किसी को किसी ख़ास इलाक़े के कल्चर का पाबंद बनाना शरीअत का आदेश नहीं है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आपके सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करने आया हो और पहले उसका लिबास तबदील करवाया हो। अबू-जहल और अबू-लहब जो लिबास पहनते थे वही लिबास सहाबा भी पहनते थे। लोग इस्लाम स्वीकार करते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी से लिबास बदलवाया गया हो। हाँ अगर किसी के लिबास में कोई ग़लती थी तो आपने उसको बता दिया कि इसमें यह ख़राबी दुरुस्त कर दो, बाक़ी लिबास ठीक है। यह शरीअत की तत्वदर्शिता और शरीअत के उद्देश्यों के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें थीं। अब इज्तिहाद के बारे में एक-दो सैद्धान्तिक और मौलिक बातें बता देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम रह गया है।
इज्तिहाद और शरीअत के मूलस्रोत
शरीअत के मौलिक आदेश तो क़ुरआन और सुन्नत से मालूम होते हैं और शरीअत के मूलस्रोत भी यही दो हैं। दो द्वितीय दर्जे के स्रोत और हैं जो प्रत्यक्ष रूप से क़ुरआन और सुन्नत से उद्धृत हैं, वे ‘इजमा’ और ‘इज्तिहाद’ हैं। इज्तिहाद तो स्वयं हदीस से साबित है और पवित्र क़ुरआन से प्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन होता है। इसलिए इज्तिहाद को एक अपने आपमें फ़िक्ह या शरीअत का एक स्थायी स्रोत माना गया है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसको स्वीकार किया। हदीस से इसका समर्थन होता है। इज्तिहाद के बहुत-से रूप हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण और मौलिक रूप ‘क़ियास’ का है। इसलिए कुछ फ़ुक़हा चौथा स्रोत ‘क़ियास’ को क़रार देते हैं और कुछ इज्तिहाद को। इन दोनों में अन्तर कोई नहीं है। इज्तिहाद एक बड़ी चीज़ है और क़ियास उसका एक महत्वपूर्ण विभाग है। इज्तिहाद का अर्थ शरीअत के किसी आदेश में परिवर्तन नहीं है। शरीअत में तो परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के आदेश निर्धारित और शाश्वत हैं और हमेशा के लिए हैं। जहाँ परिवर्तन की गुंजाइश है उसका ज़िक्र स्वयं क़ुरआन और हदीस में आ गया है। इस गुंजाइश के अलावा कोई नर्मी या परिवर्तन या संशोधन एवं निरस्तीकरण शरीअत के आदेश में नहीं हो सकता। अत: इज्तिहाद का यह अर्थ तो बिलकुल नहीं है कि जहाँ किसी आदेश पर अमल में मुश्किल पेश आए तो इज्तिहाद से उसको परिवर्तित कर दिया जाए। इज्तिहाद का अर्थ यह है कि किसी ऐसी स्थिति में जिसके बारे में पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में प्रत्यक्ष रूप से कोई आदेश मौजूद न हो, क़ुरआन और सुन्नत के आदेशों पर ग़ौर करके उसका आदेश मालूम किया जाए। शरीअत के आदेशों की खोज की इस प्रक्रिया का नाम इज्तिहाद है। यानी इज्तिहाद एक सामान्य सिद्धान्त है। इसके कई उप प्रकार हैं जिनमें एक ‘क़ियास’ है। क़ियास से मुराद यह है कि आपके सामने एक मूल आदेश है और एक बाद में पेश आनेवाली स्थिति है। दोनों में कुछ चीज़ें समान हैं। जिस क़दर समानता के आधार पर पहला आदेश आधारित है उसका आदेश आप नई स्थिति पर भी चस्पाँ कर दें। जैसे मैंने मादक पदार्थों का उदाहरण दिया था। पवित्र क़ुरआन में आया है कि ‘ख़म्र’ यानी शराब हराम है। ‘ख़म्र’ अरबी भाषा में अंगूर, गन्ने या जौ से बनी हुई शराब को कहते हैं। अब जब बाद में अफ़ीम का ज़िक्र आया तो सवाल पैदा हुआ कि अफ़ीम खाना जायज़ है कि नहीं। ज़ाहिर है अफ़ीम और शराब अलग-अलग चीज़ें हैं। फ़ुक़हा ने शराब पर ग़ौर किया कि इसमें वह कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से वह हराम क़रार दी गई है। इसका तरल पदार्थ होना तो हुर्मत (निषिद्ध होने) की दलील नहीं हो सकता। अगर द्रव्य होना हुर्मत का कारण होता तो चाय, पानी और शरबत आदि भी हराम होते। शराब के रंग का लाल होना भी हुर्मत की दलील नहीं है। शरबत का रंग और फलों के जूस भी लाल रंग के हो सकते हैं। इस तरह बहुत-सारे गुण हैं जो शराब में पाए जाते हैं। इन सब पर एक-एककर विचार किया जाए तो विचार करने से पता चल जाएगा कि शराब के हराम होने का मूल कारण क्या है। जिस गुण की वजह से शराब हराम की गई है वह गुण हर व्यक्ति की समझ में आ सकता है कि वह उसका मादक होना है। अत: अगर मादक होने से शराब हराम है तो इस वजह से अफ़ीम को भी हराम होना चाहिए। यह ‘क़ियास’ का एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि ‘क़ियास’ के आधार पर नए आदेश कैसे निकाले जाते हैं।
इज्तिहाद का शाब्दिक अर्थ है अत्यन्त प्रयास और अत्यन्त कोशिश। यह अत्यन्त का शब्द इस अर्थ में शामिल है। फ़ुक़हा ने इसकी परिभाषा की है ‘इस्तिफ़राग़ अल-वुसअ’, ‘इस्तिफ़राग़’ का अर्थ है एग्ज़ास्ट करना और ‘वुसअ’ का अर्थ हैं क्षमता। अंग्रेज़ी में इज्तिहाद के अर्थ को बयान करना हो तो यों कहा जाएगा To exhast your capacity to discover Shariah ruling about a new situation in the light of the Quran and Sunnah. यह है इज्तिहाद कि क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में किसी नई स्थिति का आदेश मालूम करने के लिए अपनी क्षमता को पूरे तौर पर प्रयुक्त कर डालना, ज्ञान और प्रतिभाओं को इस तरह निचोड़ देना कि उससे आगे क्षमता के प्रयोग करने की कोई हद या शक्ति शेष न रहे। इस प्रक्रिया का नाम इज्तिहाद है।
इज्तिहाद और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम)
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इज्तिहाद से काम लिया करते थे। स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इज्तिहाद की अनुमति दी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में बहुत-सी समस्याओं में इज्तिहाद किया और आकर आपको बताया। हज़रत अम्मार-बिन-यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का उदाहरण में दे चुका हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनके इज्तिहाद को जायज़ क़रार नहीं दिया और उनसे फ़रमाया कि तुम्हारी राय दुरुस्त नहीं थी।
इस तरह से और भी उदाहरण मौजूद हैं जिनमें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अपनी राय से एक आदेश मालूम किया। और इस आदेश को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में पेश किया गया और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसकी अनुमति दे दी। कभी-कभी ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल के प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को इज्तिहाद की अनुमति देते थे, लेकिन अंदाज़ यानी body language ऐसी होती थी कि शायद अगर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सीधे यह पूछा जाता तो आप उसका कोई और जवाब देते। यह बात ज़रा ग़ौर से सुनिएगा। एक सहाबी को सफ़र के दौरान ग़ुस्ल (स्नान) की आवश्यकता पेश आई। वहाँ पानी मौजूद था। क़ाफ़िले के कई लोगों के पास पानी था। उनसे कहा गया कि ग़ुस्ल कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर्दी बहुत है, इसलिए तयम्मुम करने को काफ़ी समझा और नमाज़ में इमामत के लिए आगे बढ़े। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो आपके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि आपने ग़ुस्ल नहीं किया, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि वे तयम्मुम करके ही नमाज़ पढ़ाएँगे। चुनाँचे उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। अब कुछ लोगों को संकोच था कि पानी की मौजूदगी में भी उन्होंने ग़ुस्ल नहीं किया, तो क्या नमाज़ हो गई कि नहीं हुई? अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सूचना मिली तो आपने उन सहाबी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया ऐ अल्लाह के रसूल! सर्दी बहुत थी। पवित्र क़ुरआन में आया है कि “अपने-आपको अपने ही हाथों हलाकत में न डालो।” मेरा ख़याल था कि अगर मैंने इस पानी से ग़ुस्ल किया तो बीमार पड़ जाऊँगा। यह जवाब सुनकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुस्कराए और ज़बान से कुछ नहीं कहा। गोया इस काम की अनुमति दे दी कि ऐसी हालत में ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम को काफ़ी समझ लेना ठीक है, लेकिन आपका मुस्कराना और ज़बाने-मुबारक से कुछ न कहना, इससे कुछ फ़ुक़हा ने यह परिणाम निकाला कि अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) यह है कि ऐसे मौक़े पर ग़ुस्ल ही किया जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग़ुस्ल न करना चाहे तो इसकी भी गुंजाइश है। अब इससे दो चीज़ें मालूम होती हैं कि अफ़ज़ल और अज़ीमत क्या है और रुख़सत की गुंजाइश कहाँ है। यह एक इज्तिहाद है जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आंशिक रूप से पसंद किया और यह इशारा भी कर दिया कि दूसरे दृष्टिकोण की भी गुंजाइश है। इस तरह के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। कुछ जगह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इज्तिहाद करने पर इतनी पसंदीदगी का इज़हार किया कि इज्तिहाद करनेवाले के लिए दुआ की कि अल्लाह उसका मार्गदर्शन करे और उसकी सहायता करे। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जब क़ाज़ी बनाकर यमन भेजा गया तो वहाँ एक घटना घटित हुई जो बड़ी दिलचस्प भी थी और फ़िक़्ही दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भी। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) एक जगह जा रहे थे तो देखा कि एक जगह बहुत हंगामा है और लोग जमा हैं। उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति ने जंगल में शेर का शिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ा खोदा था। और गढ़े को घास-फूस से बंद करके ऊपर कोई गोश्त आदि रख दिया था। अब शेर ने छलांग लगाई तो गढ़े में गिर गया। शिकारी का यही उद्देश्य था कि शेर गढ़े में गिरेगा तो उसको शिकार कर लिया जाएगा। अब इस सफलता को देखने के लिए बहुत-से लोग जमा थे। भीड़ उस गढ़े के किनारे पर खड़ी थी। भीड़ में अक्सर यह होता है कि पीछेवाले लोग आगेवालों को धकेलते हैं। पीछेवालों को पता नहीं था कि आगेवाले किस हद तक किनारे पर खड़े हैं। चुनाँचे धक्के से एक साहब गढ़े में गिर गए और शेर ने उनको दबोच लिया। इस आदमी को बचाने के लिए एक और आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, वह भी गढ़े में गिर गया। उसने तीसरे का और तीसरे ने चौथे का हाथ पकड़ा और यों चार आदमी ऊपर तले गढ़े में गिर गए। ज़ाहिर है चारों को शेर ने फाड़ खाया, क्योंकि वह भूखा भी था, भोजन ही की तलाश में आया था और ग़ुस्से में भी था।
अब सवाल यह पैदा हुआ कि इन चार आदमियों के ख़ून का ज़िम्मेदार कौन है। विभिन्न लोग विभिन्न बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि जिसने गढ़ा खोदा है वह ज़िम्मेदार है। किसी ने कहा कि जिसने पीछे से धक्का दिया वह ज़िम्मेदार है। अब भीड़ में क्या पता कि किसके धक्के से यह आदमी गिरा था। फिर चार आदमी एक के बाद एक गिरे थे। एक को सीधे शेर ने पकड़ा था, दूसरे को पहले आदमी ने, तीसरे को दूसरे ने और चौथे को तीसरे ने पकड़ा था। अपनी जान बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने निर्देश दिया कि इन चार आदमियों की दियतों के चार विभिन्न आदेश होंगे। विस्तार से बताने का यह मौक़ा नहीं। एक व्यक्ति की दियत पूर्ण रूप से बैतुलमाल पर होगी। एक व्यक्ति की दियत एक चौथाई वे लोग देंगे जो यहाँ मौजूद हैं और तीन चौथाई वह आदमी देगा जिसने उसका हाथ पकड़ा। अगले दो आदमियों की दियत को भी इस तरह वितरित किया और बहुत बौद्धिक तर्कों के साथ इस फ़ैसले को स्पष्ट किया। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सूचना हुई। आपने अत्यन्त ख़ुशी का इज़हार किया और कहा कि अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं। और क्यों न करते। आख़िर सबसे बेहतर फ़ैसला करनेवाले अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही थे और वही इतना अच्छा फ़ैसला कर सकते थे। यह गोया हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इज्तिहाद था जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुत पसंद किया।
बाद के ज़मानों में इज्तिहाद
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने में इज्तिहाद इस दृष्टि से बहुत प्रोत्साहित करनेवाला था कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इसकी स्वीकृति या इसको सुधारने के लिए मौजूद थे और यों तुरन्त ही हर ग़लती का सुधार हो जाता था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इसकी अब कोई सम्भावना नहीं रही है। अब इसका सुधार या तो इजमा के द्वारा हो जाता है कि एक से अधिक इज्तिहादात थे, चिन्तन-मनन के बाद उनमें से एक पर इजमा हो गया, यों शेष इज्तिहाद, जो बज़ाहिर कमज़ोर थे समाप्त हो गए और एक इज्तिहाद, जो बज़ाहिर ज़्यादा मज़बूत था, शेष रह गया। लेकिन अगर इजमा न हो, तो अब उसका आधार तर्क की दृढ़ता पर है। जिसका तर्क जितना मज़बूत और व्यक्तित्व जितना परहेज़गार और दीनदार है, उसकी दृष्टि से उसके इज्तिहादात को स्वीकार्य या अस्वीकार्य क़रार दिया जाएगा। मुस्लिम समाज ने जिन बुज़ुर्गों के इज्तिहादात को उनके नैतिक आचरण, तक़्वा (परहेज़गारी) और चरित्र की वजह से स्वीकार्य समझा वे प्रसिद्ध एवं जाने-माने हैं। उनमें फ़िक़्ही मसलकों के संस्थापक इमाम और दूसरे फ़ुक़हा शामिल हैं। ऐसे फ़ुक़हा के इज्तिहादात भी स्वीकार किए गए कि जो किसी फ़िक़ही मसलक के संस्थापक तो नहीं हुए, लेकिन उनकी हैसियत इतनी असाधारण है कि आज भी लोग उनके इज्तिहादात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इब्ने-तैमिया और इब्ने-क़ैय्यिम का व्यक्तित्व इतना असाधारण है कि लोग आज तक उनके विचारों और इज्तिहादात की पैरवी कर रहे हैं। इब्ने-तैमिया और इब्ने-क़य्यिम अपने-आपमें किसी फ़िक़ही मसलक के संस्थापक नहीं हैं, लेकिन वे इतनी बड़ी शख़्सियतें हैं कि उनके इज्तिहादात को दुनिया में लाखों-करोड़ों लोग मानते हैं। शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी किसी फ़िक़ही मसलक के संस्थापक नहीं हैं, लेकिन बहुत-से लोग उनके इज्तिहादात की पैरवी करते हैं।
मुज्तहिदीन के बहुत-से दर्जे हैं। वे सब एक दर्जे के नहीं थे। हर फ़िक़्ह और हर मसलक में मुज्तहिदीन का काम और उसका महत्व विभिन्न दर्जे और विभिन्न अंदाज़ रखता है। जब शुरू का ज़माना था, यानी दूसरी तीसरी सदी हिजरी का ज़माना था, तो इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के सामने मौलिक रूप से दो काम थे। उदाहरणार्थ जब इमाम शाफ़िई (रह॰), इमाम मालिक (रह॰) और उस दौर के सब लोग कार्य में व्यस्त थे तो उनके सामने मौजूद मौलिक कामों में से एक महत्वपूर्ण काम यह था कि पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के आदेशों की व्याख्या करने के उसूल तैयार करें और यह बताएँ कि क़ुरआन और सुन्नत से आदेश कैसे निकाले जाएँ, पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के किसी आदेश में टकराव मालूम हो तो उसको कैसे दूर किया जाए। पवित्र क़ुरआन की दो आयतों में कोई टकराव मालूम हो तो उसको कैसे दूर किया जाए। यानी आरम्भिक दौर के फ़ुक़हा को शरीअत की व्याख्या, शरीअत की समझ और दो परस्पर भिन्न प्रतीत होनेवाले आदेशों में सामंजस्य स्थापित करने से सम्बन्धित मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने थे। उन मौलिक प्रश्नों को आप basic structural questions कह सकते हैं।
मुस्लिम समाज को आरम्भिक दौर में तात्कालिक रूप से कुछ मौलिक समस्याओं का सामना था। इस्लामी राज्य की फैलती हुई सीमाएँ और इस्लामी समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के सामने जो समस्याएँ सामने आ रही थीं, उनका जवाब तलाश करना इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के सामने दूसरा महत्वपूर्ण और बड़ा काम था। यानी इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) दो प्रकार की आवश्यकताओं का सामान कर रहे थे। उन लोगों में से किसने कितना काम किया, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। उनमें से कुछ के काम का रिकार्ड मौजूद है और कुछ का मौजूद नहीं है। क़ाज़ी इब्ने-अबी-शबरमह बहुत बड़े फ़क़ीह थे और एक बड़े मसलक के संस्थापक थे, लेकिन समय ने उनके काम को शेष नहीं रहने दिया। उन्होंने स्वयं कोई किताब नहीं लिखी और अगर उनकी कोई रचना थी भी तो आज हम तक पहुँची नहीं हैं। और जब हम तक पहुँची नहीं हैं तो हम उनके काम के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उनके काम का प्रकार क्या था। इमाम मालिक (रह॰), इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰), इमाम शाफ़िई (रह॰) और उनके शिष्यों की किताबें हम तक पहुँचीं तो हमें मालूम है कि उनका काम किस प्रकार का था। इसलिए यह मौलिक काम जो structural प्रकार का था, यह हमारे पास मौजूद है।
इज्तिहाद की अनेक सतहें
ये तो इज्तिहाद की एक सतह थी जो दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में पूरी हो गई। अब इस सतह पर काम करने की आवश्यकता नहीं रही। अगर कोई व्यक्ति इस सतह पर दोबारा यही काम करेगा तो या तो इसी परिणाम तक पहुँचेगा जिसपर ये लोग पहले से पहुँच चुके हैं। उदाहरणार्थ एक समस्या यह आई कि ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी है कि नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उसपर अमल करना ज़रूरी नहीं है, उसपर अमल नहीं होगा। वह हदीस जो किसी एक सहाबी ने किसी एक ताबिई से बयान की हो और उन एक ताबई ने किसी एक तबअ ताबिई से बयान की हो, जो तीन मरहलों पर एक-एक आदमी के ज़रिये आई हो वह ख़बरे-वाहिद कहलाती है। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने किताब ‘अर-रिसाला’ में कोई सत्तर-पचहत्तर तर्क दिए हैं और साबित किया है कि ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने भी कहा कि ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह इमाम मालिक (रह॰) ने भी ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी क़रार दिया है। इसके बाद ख़बरे-वाहिद का पालन करने के लिए ज़रूरी होना तय हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति इस मामले में इज्तिहाद करेगा तो क्या कहेगा। यही कहेगा कि ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी है या कहेगा कि अमल करना ज़रूरी नहीं है। अगर वह अपने नए सिरे से इज्तिहाद के परिणामस्वरूप यह राय क़ायम करे कि ख़बरे-वाहिद पर अमल करना ज़रूरी नहीं है तो फिर सवाल होगा कि बिलकुल सिरे से ही अमल करना ज़रूरी नहीं है या कुछ परिस्थितियों में अमल किया जाएगा और कुछ में नहीं किया जाएगा। यह किसी ने नहीं कहा कि ख़बरे-वाहिद पर सिरे से अमल करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की पनाह! कौन मुसलमान यह कह सकता है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन का अनुपालन ज़रूरी नहीं है। उसपर अमल करना कुछ परिस्थितियों में ज़रूरी है और कुछ में नहीं है। जिन परिस्थितियों में अमल करना ज़रूरी है उनकी निशानदेही कुछ फ़ुक़हा ने की, और जिन परिस्थितियों में नहीं है उसकी भी निशानदेही कर दी। अब अगर आज कोई इस मसले पर इज्तिहाद करेगा तो उन तीनों में से ही कोई दृष्टिकोण अपनाएगा। ये तीनों दृष्टिकोण पहले ही अपनाए जा चुके हैं। इसी तरह एक सवाल यह पैदा हुआ कि पवित्र क़ुरआन में आदेशात्मक मुद्रा में जो निर्देश आए हैं कि यह और यह काम करो, वे क्या अनिवार्यता साबित करने के लिए हैं, क्या जायज़ साबित करने या मंदूब (अच्छा) और मुस्तहब (पसन्दीदा) साबित करने के लिए हैं। जहाँ आदेशों का ज़िक्र है तो ये तीन ही शक्लें सम्भव हैं। चौथी कोई शक्ल तो हो नहीं सकती। यह तो कोई नहीं कह सकता कि पवित्र क़ुरआन में कोई आदेश हुक्म देने के अन्दाज़ में दिया गया हो और उससे कार्य का निषेध या कराहत (अप्रिय होना) मुराद हो। ऐसी बात तो कोई भी नहीं कहेगा। जो शेष तीन स्थितियाँ सम्भव हैं तो वे तीनों कही जा चुकी हैं और तर्क भी बयान हो चुके हैं। अब जो आदमी इज्तिहाद करेगा तो उन तीनों में से कोई एक बात करेगा जो पहले ही कही जा चुकी। तो यह सारी मश्क़ मात्र बेकार बात है। नई बात कहेगा तो वह स्वीकार्य नहीं इसलिए कि अरबी भाषा इसे सहन नहीं कर सकती। मानव-बुद्धि इसकी अनुमति नहीं देगी कि सर्वोच्च अल्लाह कह रहा है कि यह काम करो और आप कहें कि यह न करने का आदेश है। इस तरह की मौलिक समस्याएँ तय हो चुकी हैं, अब उनको दोबारा खोलने re-open करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आंशिक समस्याएँ मुस्लिम समाज को पेश आती रहेंगे। जब तक इंसान मौजूद है और जब तक मुसलमान मौजूद हैं तो असीमित आंशिक समस्याएँ पेश आती रहेंगे। उनमें इज्तिहाद भी होता रहेगा। गोया इज्तिहाद की दो सतहें तो इतनी स्पष्ट हैं जो हर एक को नज़र आ सकती हैं। जहाँ तक इज्तिहाद की पहली सतह का सम्बन्ध है उसको ‘इज्तिहादे-मुतलक़’ कहा जाता है। इसके इज्तिहाद करनेवाले को ‘मुज्तहिदे-मुतलक़’ कहते हैं। मुज्तहिदे-मुतलक़ का काम लगभग समाप्त हो गया। जब फ़ुक़हा ने यह लिखा कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया, तो उनकी मुराद यही थी कि इज्तिहादे-मुतलक़ का दरवाज़ा बंद हो गया। वास्तव में उसकी अब आवश्यकता नहीं रही। इसलिए कि जो काम इज्तिहादे-मुतलक़ के ज़रिये करना अभीष्ट था वह सारा-का-सारा किया जा चुका। अब दोबारा इज्तिहादे-मुतलक़ की प्रक्रिया दोहराना अंग्रेज़ी मुहावरे के अनुसार पहिये को दोबारा ईजाद करने के समान है। इसलिए यह दरवाज़ा व्यवहारत: बंद हो चुका है।
इसके बाद ‘इज्तिहादे-मुंतसिब’ का दर्जा है। ‘इज्तिहादे-मुंतसिब’ करनेवाले को ‘मुज्तहिदे-मुंतसिब’ कहते हैं। यानी वह इज्तिहाद जो किसी बड़े फ़क़ीह के इज्तिहाद की शैली और इस्तिदलाल (तर्क शैली) के तरीक़े को सामने रखते हुए विवरण तैयार करने के लिए किया जाए। जैसा इमाम मुहम्मद और इमाम अबू-यूसुफ़ ने इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के सिद्धान्तों के अनुसार इज्तिहाद किया। इमाम मुज़नी और रबी-बिन-सुलैमान ने इमाम शाफ़िई (रह॰) के सिद्धान्तों के अनुसार किया। असद-बिन-फ़ुरात और यहया-बिन-यहया ने इमाम मालिक (रह॰) की शैली के अनुसार किया। यानी मौलिक धारणाओं और सिद्धान्तों में वे अपने इमाम के दृष्टिकोण के अनुयायी हैं। लेकिन इसके अन्दर विस्तृत विवरण उपलब्ध करने का जो काम है, वह उन्होंने किया। यह मुज्तहिद का दूसरा दर्जा है और ऐसा इज्तिहाद करनेवाले को मुज्तहिदे-मुंतसिब कहते हैं।
तीसरा दर्जा मुज्तहिद फ़िल-मसाइल का है, यानी जो आंशिक समस्याओं में इज्तिहाद करता है। समस्याएँ पेश आती रहेंगी और नए इज्तिहादात की आवश्यकता पेश आती जाएगी। यों मुज्तहिद फ़िल-मसाइल हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये तीन दर्जात तो वे हैं जिनको तमाम फ़ुक़हा स्वीकार करते हैं। तीसरा दर्जा हमेशा खुला रहेगा। दूसरे दर्जे की जब आवश्यकता पेश आएगी उस समय काम लिया जाएगा और जब आवश्यकता नहीं होगी तो काम लेने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसमें सावधानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर इज्तिहाद का दरवाज़ा चौपट खोल दिया जाए और हर व्यक्ति उसमें दाख़िल होने लगे तो फिर शरीअत के मामलात मज़ाक़ बन जाएँगे। शरीअत की व्याख्या का मामला कम इल्मों के हाथ आ जाएगा और इससे मुस्लिम समाज में कनफ़्यूज़न और उलझाव फैलेगा।
कम समझ आलिमों के इज्तिहाद के मुक़ाबले में बेहतर यह है कि जो पिछले विश्वसनीय बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनके इज्तिहाद पर भरोसा किया जाए और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए। इसलिए इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इज्तिहाद के बारे में कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनका सख़्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और कोशिश की गई है कि इन सीमाओं के अन्दर रहते हुए इज्तिहाद किया जाए।
नई पेश आनेवाली समस्याओं में इज्तिहाद आज भी जारी है, आइन्दा भी जारी रहेगा। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दुनिया से जाने से पहले इसकी अनुमति दी थी। हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) के तर्ज़े-अमल को पसंद किया था। इसके बाद हज़रत मुआज़ की अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मुलाक़ात नहीं हुई (जैसा कि आपने फ़रमाया था), इसलिए इज्तिहाद के ज़रीये समस्याओं का समाधान तलाश करना एक तरह से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वसीयत भी है और नबी की वसीयत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
सवालात
सवाल : ‘इस्तेहलाकी’ और ‘इस्तेमाली’ चीज़ों के बारे में दोबारा बता दें।
जवाब : इंसान की मिल्कियत में जो चीज़ें होती हैं और माल की जितनी भी क़िस्में हैं उनको दो क़िस्मों में विभाजित किया जा सकता है। एक माल वह है जिसको आपने उपभोग करके समाप्त कर दिया। यानी consume कर दिया और वह समाप्त हो गया। जैसे यह पानी मैंने आपसे उधार लिया था। इसको मैंने पी लिया और यह समाप्त हो गया। अब अगर आप इस पानी को वापस माँगें तो मैं आपको वापस नहीं दे सकूँगा। इसलिए कि वह तो समाप्त हो गया और मैं इसको वापस नहीं कर सकता। मैं इस जैसा कुछ और पानी आपको वापस कर सकता हूँ। इसी मात्रा में वापस करूँगा। यह दूध हो सकता है, शहद हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है। यह चीज़ें ‘इस्तेहलाकी’ चीज़ें हैं। इसको आपने इस्तेमाल करके समाप्त कर दिया, उपभोग कर लिया, और consume कर दिया। ‘इस्तेहलाकी’ मुराद है consumable. दूसरी चीज़ है ‘इस्तेमाली’ यानी usable. उदाहरणार्थ मैंने यह गिलास आपसे आरियतन (इस्तेमाल के लिए) माँगा और इस्तेमाल करके वापस दे दिया। जैसा लिया था वैसा ही वापस कर दिया, जो चीज़ ली थी वही चीज़ वापस कर रहा हूँ, इस जैसी कोई चीज़ वापस नहीं कर रहा हूँ। ‘रिबा’ का उदाहरण मैंने यह दिया था कि ‘रिबा’ उन चीज़ों के लेन-देन में होता है जो ‘इस्तेहलाकी’ हों। ‘इस्तेमाली’ चीज़ों के लेन-देन में अक्सर ‘रिबा’ नहीं होता। यह एक आम उसूल है और इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ‘रिबा’ के अधिकतर आदेश ‘इस्तेहलाकी’ चीज़ों में जारी होते हैं, ‘इस्तेमाली’ चीज़ों में जारी नहीं होते।
✩
सवाल : सामूहिक सुन्नतों को व्यक्तिगत सुन्नतों पर वरीयता प्राप्त है। फिर ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ को ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ पर वरीयता क्यों नहीं?
जवाब : ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ को निश्चय ही ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ पर वरीयता प्राप्त है। दर्जा ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ का ही बड़ा है। लेकिन चूँकि इंसान कमज़ोर है इसलिए सर्वोच्च अल्लाह ने कुछ परिस्थितियों और कुछ मामलों में इंसान को अनुमति दी है कि वह ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ को प्राथमिकता दे और ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ को अस्थायी रुप से नज़रअंदाज या स्थगित कर दे। यह बात केवल अनुमति की है अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) की नहीं है।
✩
सवाल : पिछले लेक्चर में आपने इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के तरीक़े-तदरीस (शिक्षण शैली) का ज़िक्र किया जो बहुत दिलचस्प लगा। उनके पढ़ाने का यह तरीक़ा किसी किताब में दर्ज है या यह आपका अपना ख़याल है?
जवाब : ये उनके तमाम वृत्तान्त लेखकों ने लिखा है। पुराने ज़माने में अक्सर लोगों का तरीक़ा यही होता था। आप इमाम मुहम्मद की किताबें देखें, ख़ास तौर पर उनकी दो किताबें, यानी ‘किताबुल-अस्ल’, जो ‘किताबुल-मबसूत’ भी कहलाती है और दूसरी किताब पाँच छः भागों में है ‘किताबुल-हुज्जति अला अहलिल-मदीनति’, जिसमें उन्होंने इमाम मालिक (रह॰) और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के दरमियान इख़्तिलाफ़ी मसाइल (वे समस्याएँ जिनमें फ़ुक़हा के बीच मतभेद हो) पर बहस की है। इन सब बुज़ुर्गों का तरीक़े-तदरीस यह होता था कि पहले वे कहते थे कि “क़ा-ल अबू-हनीफ़ा (रह॰)”, यानी अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने यह कहा, “क़ुलना”, हमने यह कहा, “क़ा-ल” उन्होंने कहा, “क़ुलना” हमने कहा। बीस-बीस पृष्ठों तक यही होता है कि क़ा-ल, क़ुलना, उन्होंने यह कहा और हमने यह कहा। इस पूरे वार्तालाप में सबके बारे में तफ़सील मौजूद होती है कि किसने क्या कहा। फिर आख़िर में एक बात पर मतैक्य हो जाता है। इमाम शाफ़िई (रह॰) की ‘किताबुल-उम्म’ पढ़ें। उसमें आधी से ज़्यादा किताब इन बहसों पर आधारित है कि मैं इराक़ गया तो वहाँ एक फ़क़ीह से मेरी बहस हुई। उन्होंने यह कहा, मैंने यह कहा, उन्होंने यह कहा और मैंने यह कहा। अन्ततः वह मान गए कि तुम सही कह रहे हो। यह तो सब किताबों में लिखा है। इसमें से ख़ुद कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं, आप कोई भी पुरानी किताब उठाकर देख लें। ‘अल-मुदव्वना’ देख लें उसमें भी ऐसा ही है।
✩
सवाल : शराब और अफ़ीम के अलावा भी क्या क़ियास का कोई उदाहरण है?
जवाब : सारे ही फ़िक़ही आदेश क़ियास के आधार पर हैं। लेकिन यह उदाहरण चूँकि बहुत आसान था इसलिए मैंने दे दिया।
✩
सवाल : कल रोज़ा इफ़्तार करने के हवाले से ‘इलल-लैल’ के बारे में बात करते हुए सूरज की टिकिया अस्त होने या उसका प्रभाव समाप्त होने पर बात हुई। ‘लैल’ के स्पष्टीकरण के लिए क्या इन चीज़ों को देखा जाएगा या नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत देखी जाएगी। इस मामले में स्पष्ट उल्लेख मौजूद हैं जिनमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जल्द इफ़्तार करने का आदेश दिया है। स्वयं भी जल्दी की। ऐसे में क्या एक गिरोह की राय दुरुस्त और दूसरे गिरोह की राय ग़लत क़रार नहीं पाएगी?
जवाब : मेरे नज़दीक पहले गिरोह की राय दुरुस्त है और दूसरे गिरोह की राय कमज़ोर है। लेकिन इसके दुरुस्त होने की सम्भावना मौजूद है। मेरा मतलब यह है कि यह तो ‘लैल’ के शब्द की एक समझ है जिसको आप ग़लत कह सकते हैं। मैं स्वयं भी इसको ग़लत समझता हूँ, लेकिन इसको गुमराही कहना और इसको मसला बनाना दुरुस्त नहीं है। यह न कहें कि यह इस्लाम से फिर जाना है। यह तो समझ का मामला है जिसमें ग़लती भी हो सकती है। वे हदीसें दुरुस्त हैं जिनमें रोज़ा जल्दी इफ़्तार करने का आदेश है। वे उसकी व्याख्या यह बयान करते हैं कि जैसे ही रात शुरू हो जाए फ़ौरन रोज़ा इफ़्तार करो। जब रात शुरू हो जाए तो और देर बिलकुल न करो और फ़ौरन रोज़ा इफ़्तार कर लो। उनकी राय में जब तक शफ़क़ (उषा की लालिमा) मौजूद है रात शुरू नहीं हुई। अत: जब रात ही शुरू नहीं हुई तो आपने इफ़्तार कैसे कर लिया।
अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) का दृष्टिकोण यह है कि जब सूरज की टिकिया छिप जाए, तो समझा जाएगा कि रात शुरू हो गई। कुछ हंबली फ़ुक़हा का कहना है कि अगर दरमियान में कोई पहाड़ हो, और सूरज की टिकिया उस पहाड़ के पीछे छुप गई। आपको उसकी शफ़क़ भी नज़र नहीं आ रही है तो क्या आपको पहाड़ पर चढ़कर देखना होगा कि सूरज वाक़ई डूब गया है या नहीं? पुराने ज़माने में घड़ियाँ तो होती नहीं थीं। तो अगर पहाड़ पर चढ़-चढ़कर देखना पड़े तो इफ़्तार तो धरे-का-धरा रह जाएगा। इसलिए इमाम अहमद (रह॰) और उनके हम-मसलक फ़ुक़हा ने कहा कि नहीं, ऊपर जाने की शर्त ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी रात हो जाएगी। यह उन्होंने एक राय दे दी। अब हो सकता है कि पहाड़ के पीछे सूरज मौजूद हो। जो लोग हंबली नहीं थे उन्होंने इसका मज़ाक़ उड़ाया और तरह-तरह के लतीफ़े बनाए। एक साहब ने एक हंबली से कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा था। रोज़ा इफ़्तार करने के लिए उतरा। सूरज ऊँट के पीछे छिप गया था तो मैं समझा कि सूरज डूब गया। आपके फ़िक़्ह के अनुसार खड़े होकर देखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। रोज़ा इफ़्तार करने के बाद ऊँट चल पड़ा, तो पता चला कि सूरज तो मौजूद है। बताइए मेरा रोज़ा हुआ कि नहीं? यह एक दूसरी इंतिहा है। इमाम अहमद का उद्देश्य यह नहीं था। उनका उद्देश्य यह था कि शरीअत ने ग़ैर-ज़रूरी मुश्किल का आदेश नहीं दिया। हरज का आदेश नहीं दिया। अगर इस दौर में या आज के दौर में आपके पास घड़ी नहीं, न जंतरी है और दरमियान में इतना ऊँचा पहाड़ है जिसपर चढ़ने के लिए दो तीन घंटे चाहिएँ, तो क्या शरीअत कहती है कि आप पहाड़ पर चढ़कर देखें। इमाम अहमद (रह॰) फ़रमाते हैं कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन अब इसको इस इंतिहा पर ले जाना कि ऊँट के साये में बैठकर आप कहें कि सूरज डूब गया है, तो यह नाइंसाफ़ी है।
✩
सवाल : शरीअत के आदेशों के पीछे तत्वदर्शिताओं के जो तर्क किताबों में मौजूद हैं, उन किताबों के नाम दोबारा बता दें।
जवाब : अगर आप अरबी जानते हैं तो ‘क़वाइदुल-अहकाम फ़ी मसालिहिल-अनाम’ पढ़ें। यानी इंसानों के निहितार्थों के नियमों का बयान। यह अल्लामा इज़ुद्दीन-बिन-अब्दुस्सलाम की किताब है। दूसरी किताब इमाम शातबी की ‘अल-मुवाफ़क़ात’ है। यह चार भागों में है। तीसरी किताब हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी की ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ है, ख़ास तौर पर इसका दूसरा भाग।
✩
सवाल : अगर किसी का गर्भपात हो जाए और उसको माहवारी का ज़माना न हो तो क्या ऐसी औरत रोज़े रख सकती है?
जवाब : जी हाँ, अगर गर्भपात के बाद उसको ख़ून का रिसाव न हो रहा हो तो रोज़ा रख सकती है।
☆
सवला : जैसा कि आपने बताया कि सफ़र के दौरान आधी नमाज़ होगी। लेकिन मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी जगह उन्नीस दिन क़ियाम करें तो आधी नमाज़ है। अगर उन्नीस दिन से ज़्यादा है तो पूरी नमाज़ अदा करनी होगी।
जवाब : यह दुरुस्त है। मैंने सफ़र का उदाहरण दिया था। सफ़र वही है जो नियुक्त अवधि से कम हो। निर्धारित अवधि उन्नीस दिन नहीं, बल्कि पंद्रह दिन है।
✩
सवाल : मिल्कियते-नाक़िस को आपने सही तरह से नहीं समझाया।
जवाब : जो मिल्कियते-ताम नहीं है वह मिल्कियते-नाक़िस है। एक चीज़ समझ में आ जाए, उदाहरणार्थ रात की परिभाषा की जाए कि रात ऐसी होती है तो उसके अलावा जो समय है वह ज़ाहिर है कि दिन का समय है। यह तो एक बौद्धिक बात है। मिल्कियते-ताम को समझ लेना काफ़ी है। जो मिल्कियते-ताम नहीं है वह मिल्कियते-नाक़िस है।
Recent posts
-

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -

फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025 -

इल्मे-फ़िक़्ह के विभिन्न विषय (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 4)
25 February 2025