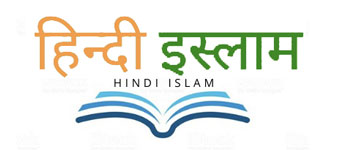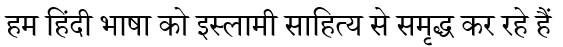इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
-
फ़िक़्ह
- at 17 March 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
आज की चर्चा का विषय है ‘इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून’। इस चर्चा में इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून की मौलिक धारणाएँ, तत्वदर्शिता और उद्देश्य चर्चा में आएँगे। यों तो फ़िक़्हे-इस्लामी एक असीम समुद्र है और इसके बहुत-से विषय और उप विभाग हैं जिनमें हर एक अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लेक्चर्स के इस सिलसिले में फ़िक़्हे-इस्लामी के उप अध्यायों में से तीन अध्यायों पर अलग-अलग चर्चा होगी।
एक इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून, दूसरा इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून। और तीसरा इस्लाम का व्यापार-क़ानून एवं अर्थशास्त्र। इन तीन विभागों के चयन का कारण यह है कि आजकल आम तौर पर ये तीन विभाग बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं और जब भी इस्लाम या शरीअत के लागू करने की बात होती है, तो आम तौर से जो सवालात किए जाते हैं वे अधिकतर इन्हीं तीन विभागों से सम्बन्धित होते हैं।
यों तो इस्लामी क़ानून के बहुत-से विभाग हैं जिनमें से आठ बड़े मैदानों का ज़िक्र मैंने एक चर्चा में विस्तार से किया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये तीन विभाग अत्यन्त महत्व रखते हैं और आधुनिक काल के सन्दर्भ में इन तीन विभागों के बारे में बहुत-से सन्देह उठाए जाते हैं। इस्लाम के बारे में जो ग़लत-फ़हमियाँ पाई जाती हैं वे भी प्रायः इन्हीं तीन विभागों के बारे में होती हैं। जो सन्देह ज़ेहनों में कुलबुलाते हैं वे भी अधिकतर इन्हीं तीन विभागों से सम्बन्धित हैं। इसलिए इन तीन विभागों को अलग-अलग शीर्षकों के तौर पर चुना गया है। चुनाँचे आज की चर्चा इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून पर है। आगे दो चर्चाएँ इस्लाम के फ़ौजदारी और व्यापारिक क़ानूनों पर होंगी। इन चर्चाओं में इन क़ानूनों की मौलिक धारणाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों की निशानदेही की जाएगी।
ज़ाहिर है एक घंटे की इस संक्षिप्त चर्चा में न तो इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानूनों पर विस्तार से विचार व्यक्त किये जा सकते हैं। न उसके आदेशों और विभागों का विस्तृत विवरण पेश किया जा सकता है और न वे सीमाएँ पूरी व्याख्या के साथ बयान की जा सकती हैं, जिनको सामने रखकर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने-अपने ज़मानों में इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून के विस्तृत आदेश संकलित किए। इसलिए समय की इस तंगी के सामने उन महत्वपूर्ण विषयों का एक सरसरी परिचय ही पेश किया जा सकता है।
कुछ आरम्भिक बातें
इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून पर बात करने से पहले कुछ आरम्भिक बातें करना अनिवार्य है। इन आरम्भिक बातों में कुछ ऐसी मौलिक और सैद्धान्तिक धारणाओं और उद्देश्यों की निशानदेही अभीष्ट है जो शरीअत के इन आदेशों में सामने रखे गए हैं। इस्लामी शरीअत एक स्वाभाविक क़ानूनी व्यवस्था है। यह इंसान की तमाम जायज़ और स्वाभाविक आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखती है। इसमें इंसानों की कमज़ोरियों को भी सामने रखा गया है। इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का भी ख़याल रखा गया है और इंसानों की तमाम जायज़ और माक़ूल अपेक्षाओं की पूर्ति का सामान भी उपलब्ध किया गया है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति और अपेक्षाओं को पूरा करने का यह सामान एक सन्तुलन के अंदाज़ में किया गया है। दुनिया की अधिकतर व्यवस्थाओं में मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिनमें कभी-कभी टकराव और कश्मकश की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, पूरे तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि उसके किसी एक पहलू को दूसरे किसी पहलू पर प्राथमिकता दी गई जिसका परिणाम यह निकला कि अगर एक पहलू से इंसानी अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया तो दूसरे कई पहलुओं की अपेक्षाएँ प्रभावित हो गईं।
चुनाँचे आधुनिक काल के पश्चिमी क़ानूनों ने इंसान के केवल एक पहलू को सामने रखा और यह बाह्य सामूहिक जीवन का वह पहलू है जिसपर अदालतों में चर्चा हो सकती है या जिसपर दो व्यक्तियों के दरमियान कोई मतभेद या अधिकारों तथा दायित्वों के आधार पर कोई विवाद पैदा हो सकता है। ज़ाहिर है यह मानव-जीवन का एक अत्यन्त संक्षिप्त और सीमित पहलू है। हममें से शायद ही किसी को किसी अदालत में जाने और मुक़द्दमा लड़ने का संयोग हुआ हो। बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी संख्या कुछ प्रतिशत से ज़्यादा हरगिज़ नहीं जिनको अपने मामलात अदालतों में ले जाने पड़ते हैं या जिनको अदालतों में पेश होना पड़ता है। हर सभ्य देश में इंसानों की बड़ी संख्या वह होती है, जो स्वयं क़ानून का पालन करते हैं। जो ख़ुद से लोगों के अधिकारों का ध्यान रखते हैं और उनको अदालतों और कचहरियों में पेश होना नहीं पड़ता। इससे पता चला कि क़ानून का वह पहलू जो अदालती कार्रवाई और हस्तक्षेप को बहुत महत्व देता है, वह मानव-जीवन के एक या दो या तीन प्रतिशत से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मानव-जीवन के शेष सत्तानवे या अट्ठानवे प्रतिशत पहलू वे हैं जो अदालतों और देश के क़ानून के प्रत्यक्ष रूप से कार्य-क्षेत्र में नहीं आते। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी क़ानून ने मानव-जीवन के तीन, चार या पाँच पहलुओं को तो बहुत महत्व दिया है, लेकिन शेष पच्चानवे प्रतिशत पहलुओं को छोड़ दिया है।
इसके विपरीत संसार के धर्मों ने यह दावा किया कि वह मानव-जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देंगे और इसको इस तरह संगठित करेंगे कि इंसान आध्यात्मिक दृष्टि से एक पूर्ण स्रष्ट जीव बन जाए। लेकिन जिन लोगों ने इंसान के आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान दिया उन्होंने इंसान के बाह्य या शारीरिक जीवन को अनदेखा कर दिया। इंसान की भौतिक अपेक्षाओं को भुला दिया और यह बात सामने न रखी कि इंसान की शारीरिक अपेक्षाएँ भी हैं। इंसान एक परिवार का व्यक्ति भी है। इंसानों के कारोबार और नौकरियाँ भी हैं। जब तक इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, उस व्यवस्था में न तो मध्यमार्ग पैदा हो सकता है और न सन्तुलन पैदा हो सकता है। इसलिए इस्लाम का सबसे पहला और सर्वप्रथम लक्ष्य यह है कि मानव-जीवन को एक पूर्ण मानव-जीवन के तौर पर लिया जाए। और इंसान के जीवन के तमाम पहलुओं को इस तरह सन्तुलन और मध्यमार्ग उपलब्ध किया जाए कि मानव-जीवन का कोई विभाग मार्गदर्शन और अनुशासन से ख़ाली न रहे। यह सबसे पहला आधार है जो इस्लामी क़ानून के संवैधानिक और प्रशासनकि धारणाओं को समझने के लिए अपरिहार्य है।
दूसरी मौलिक चीज़ जो सामने रहनी चाहिए वह यह है कि पवित्र क़ुरआन से पता चलता है और हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसको और स्पष्ट कर दिया कि इंसान के जीवन में सन्तुलन और मध्यमार्ग उसी समय पैदा हो सकता है जब उसमें अनुशासन हो। अगर अनुशासन न हो तो अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था और अच्छे-से-अच्छा क़ानून सन्तुलन और मध्यमार्ग उपलब्ध नहीं कर सकता। आप कोई भी अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था सोच-सोचकर संकलित कर लें जिसमें सन्तुलन और मध्यमार्ग की तमाम अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया हो, जिसमें सन्तुलन और एतिदाल उपलब्ध करनेवाले सारे उसूल जमा कर दिए गए हों, लेकिन अगर समाज में अनुशासन नहीं है तो ऐसी स्थिति में क़ानून की उपयोगिता बहुत-सीमित होकर रह जाती है। अगर लोग क़ानून के सिद्धान्तों पर अमल न करें, न ही इन सिद्धान्तों पर कार्यान्वयन को निश्चित बनानेवाला कोई प्लेटफ़ार्म मौजूद हो तो बेहतर से बेहतर क़ानून निरर्थक और निष्परिणाम साबित होता है। इसलिए सन्तुलन और मध्यमार्ग को वास्तविक अर्थों में प्राप्त करने के लिए अनुशासन भी ज़रूरी है। यह अगर न हो तो फिर इंसान के जीवन को अव्यवस्था से कोई नहीं बचा सकता।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुसलमानों को अनुशासन का प्रशिक्षण किस तरह दिया, वह उनकी शिक्षा के हर-हर पहलू से नुमायाँ है। नमाज़ जो कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से विशुद्ध निजी इबादत है और अल्लाह और बन्दे के दरमियान सम्बन्ध को मज़बूत करने के लिए है, इसमें भी अनुशासन और सामूहिकता की जो शान है वह हर मुसलमान पर स्पष्ट है। अगर मुसलमान सफ़र के लिए जाए तो उसको निर्देश दिया गया है कि अगर दो से अधिक व्यक्ति हों, तो वे अपने में से एक को अमीर (प्रमुख) नियुक्त कर लें। यानी वह सफ़र जो विशुद्ध निजी प्रकार का हो, या शिक्षा के लिए या व्यापार या किसी भी उद्देश्य के लिए हो, उसमें भी बिना अनुशासन के सफ़र करना इस्लाम के स्वभाव के ख़िलाफ़ है और इस्लाम ने इसको पसन्द नहीं किया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस्लाम अनुशासन को कितना महत्व देता है और उसको कैसे क़ायम करता है।
एक छोटे-से घरेलू माहौल में, जिसमें आरम्भिक तौर पर दो ही व्यक्ति होते हैं, उनमें भी एक व्यक्ति इस यूनिट का प्रमुख है और दूसरा उसका सलाहकार है। लोग कहते हैं कि शरीअत ने पुरुष को क़व्वाम (प्रभारी) बना दिया है। वे यह नहीं समझते कि अगर अनुशासन को वह महत्व देना है जो इस्लाम देता है तो फिर दोनों में से कोई एक तो क़व्वाम होगा। अगर दो व्यक्तियों पर सम्मानित एक यूनिट है और इस्लाम के स्वभाव के अनुसार इसमें सन्तुलन, और अनुशासन क़ायम होना चाहिए तो दो आदमी एक ही समय में अनुशासन के ज़िम्मेदार तो नहीं हो सकते। एक ही आदमी अनुशासन का ज़िम्मेदार होगा। वह पुरुष हो या महिला हो। दोनों स्थितियों में सवाल हो सकता है कि एक को क्यों बनाया है और दूसरे को क्यों नहीं बनाया। अल्लाह ने अपनी अपार तत्वदर्शिता के तहत दोनों को बराबर रखा है। दोनों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ अपनी-अपनी मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर हैं। दोनों की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रकार में अन्तर तो ज़रूर है, लेकिन ज़िम्मेदारी के विभिन्न होने या छोटा या बड़ा होने के बावजूद दोनों की नैतिक, सामूहिक और क़ानूनी हैसियत बराबर है। एक की ज़िम्मेदारी एक दृष्टि से ज़्यादा है, तो दूसरे की ज़िम्मेदारी दूसरी दृष्टि से ज़्यादा है।
अंग्रेज़ी व्यवस्था और संविधान के अध्ययन में अगर आपको यह पढ़ने का मौक़ा मिले कि कैबिनेट क्या होती है, तो आपको पुरुष के क़व्वाम होने की हैसियत और पुरुष एवं स्त्री में समानता की बज़ाहिर टकराती धारणाओं को समझने में सहायता मिलेगी। उनका तरीक़ा यह है कि अपनी हर चीज़ को बहुत ख़ूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। पश्चिमी दुनिया के बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ और लिखनेवालों की यह आदत बन गई है कि अपनी कमज़ोर-से-कमज़ोर चीज़ को इस तरह ख़ूबसूरत बनाकर पेश करते हैं कि बहुत-से सीधे-साधे लोगों को उसकी कमज़ोरी का आभास तक नहीं होता। हमारे लोगों के लिए उनके क़लम से लिखा हुआ हर लेख, बल्कि हर हर शब्द पत्थर की लकीर के बराबर होता है। हमारी अच्छी-से-अच्छी चीज़ को भी वे इस तरह नकारात्मक अंदाज़ में बयान करते हैं कि हमारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और अपनी हर चीज़ को नकारात्मक समझने लगते हैं। उनके यहाँ सच तो यह है कि प्रधानमंत्री ही सर्वाधिकार रखता है, शेष मंत्री उसके अधीनस्थ हैं। इसमें किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं। जिसका जी चाहे जाकर उनकी व्यवस्था देख ले। लेकिन उनका दावा यह है कि तमाम मंत्री बराबर हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के दरमियान कोई अन्तर नहीं। फिर प्रधानमंत्री का इतना ऊँचा दर्जा क्यों है, इसके लिए उन्होंने जो शैली अपनाई है उसमें लिखा है— All ministers are equal and the prime minister is the first among equals. यानी सब मंत्री बराबर हैं, लेकिन जब क्रम होगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आएगा। यह लम्बा संविष्ट वाक्य मैंने यह शैली अपनाने के लिए प्रयुक्त किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह इस्लामी परिवार में पुरुष क़व्वाम है। वह अगरचे परिवार के अन्य लोगों के साथ बराबरी रखता है, लेकिन बराबरवालों में पहला दर्जा उसी का है। परिवार में जो प्रमुख है वह भी बराबर के लोगों में पहला है first among the equals है। मैं यह वाक्य प्रयुक्त करना चाहता था इसलिए मैंने यह लंबी भूमिका बाँधी।
इन दो चीज़ों के बाद जो तीसरी चीज़ पवित्र क़ुरआन के सामने है वह यह है कि इस दुनिया के जीवन में और आख़िरत के जीवन की अपेक्षाओं में सन्तुलन होना चाहिए। निस्सन्देह इस्लाम का मूल उद्देश्य आख़िरत का जीवन है। इस्लाम इंसानों को आख़िरत के जीवन ही के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन आख़िरत के जीवन की तैयारी इसी (सांसारिक) जीवन में होगी, क़ब्र में जाकर होने से तो रही। आख़िरत के लिए जो काम करना है वह इसी जीवन में करना है। मरने के बाद आख़िरत के लिए काम नहीं हो सकेगा। इसलिए यह बात इस्लाम के स्वभाव और योजना के ख़िलाफ़ है कि इस दुनिया के जीवन की अपेक्षाओं को उपेक्षित कर दिया जाए या भुला दिया जाए। यह बात पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह इतनी निरन्तरता से बयान हुई है और पवित्र क़ुरआन के आदेशों से इतनी स्पष्ट है कि इसपर किसी और तर्क की आवश्यकता नहीं। رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ “ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई दे और आख़िरत में भी भलाई दे और हमें (जहन्नम की) आग से बचा।” (क़ुरआन, 2:201) की दुआ हर मुसलमान कम-से-कम पाँच बार प्रतिदिन करता है। पवित्र क़ुरआन शायद एक मात्र आसमानी किताब है जिसने दुनिया एवं आख़िरत की भलाइयों को एक सतह पर रखा है और सर्वोच्च अल्लाह से दोनों की दुआ माँगने की नसीहत की है। “और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है,” (क़ुरआन, 28:77) इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना न भूलो और इस दुनिया में आख़िरत के लिए जो नेअमतें हैं वे भी न भूलो। इस दुनिया में जायज़ तरीक़े से जो धन-दौलत, लाभ और नफ़ा प्राप्त कर सकते हो वह प्राप्त करो। एक जगह है “इस दुनिया का सवाब भी प्राप्त करो और आख़िरत का सवाब भी प्राप्त करो, जो बेहतरीन सवाब है।” (क़ुरआन, 3:148) एक और जगह है “इस दुनिया की अच्छाइयाँ भी दे और आख़िरत में तो हम तेरी ही तरफ़ हिदायत के साथ लौटनेवाले हैं।” (क़ुरआन, 7:156) पवित्र क़ुरआन में इस तरह की दर्जनों आयतें हैं जिनमें दुनिया और आख़िरत के जीवन में मध्यमार्ग अपनाने की शिक्षा दी गई है।
दुनिया और आख़िरत में सन्तुलन और मध्यमार्ग प्राप्त करने के लिए जहाँ अनुशासन ज़रूरी है, वहाँ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। वह यह कि इंसानी समाज में कोई फ़ित्ना न हो। फ़ित्ना पवित्र क़ुरआन की एक अत्यन्त व्यापक शब्दावली है। इससे मुराद वह अव्यवस्था और अराजकता है जो इंसानों में अनुशासन को समाप्त कर दे और इंसानों की जान-माल को ख़तरे में डाल दे। पवित्र क़ुरआन फ़ित्ने को समाप्त करना चाहता है। अगर फ़ित्ना समाप्त करने के लिए दूसरे शान्तिपूर्ण साधन अपर्याप्त साबित हो जाएँ तो फिर ताक़त का प्रयोग करने की भी अनुमति है। अगर बल प्रयोग और क़ानून की ताक़त से भी फ़ित्ना समाप्त न हो और फ़ित्ना फैलानेवाले बहुत ताक़तवर हो गए हों तो उनके ख़िलाफ़ जंग करने की भी अनुमति है। क़ुरआन में कहा गया है— “उनसे युद्ध करो, यहाँ तक कि फ़ित्ना बाक़ी न रहे और दीन (धर्म) पूरा-का-पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए।” (क़ुरआन, 8:39) गोया फ़ित्ने का ख़ातिमा पवित्र क़ुरआन के मौलिक उद्देश्यों में से है और शरीअत की योजना में मौलिक महत्व रखता है।
फ़ित्ने की समाप्ति जिस अनुशासन से हो सकती है, वह हुकूमत का अनुशासन है। हुकूमत का अनुशासन फ़ित्ने की समाप्ति में सहायता देता है, बल्कि हुकूमत की स्थापना का उद्देश्य ही फ़ित्ने को समाप्त करने का है।
इस्लाम का सर्वप्रथम सामूहिक लक्ष्य
यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए और इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वह पवित्र क़ुरआन के सर्वप्रथम सामूहिक लक्ष्य की बात है, जिसको न समझने की वजह से बहुत-सी ग़लत-फ़हमियाँ पैदा होती चली जाती हैं और सोच का काँटा बदल जाता है। पवित्र क़ुरआन को आप आरम्भ से लेकर अन्त तक पढ़ लें। पूरे पवित्र क़ुरआन में कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि ऐ मुसलमानो, तुम्हारा मूल लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति है, अत: हर प्रकार के संसाधन से काम लेकर सत्ता की प्राप्ति के लिए कोशिश करो। कुर्सी पर क़ब्ज़ा कर लो, तख़्त प्राप्त करो, लोगों की गर्दनों पर शासक बन जाओ। ऐसी कोई बात पवित्र क़ुरआन की किसी सूरा, किसी आयत या किसी भी सन्दर्भ में स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से किसी भी शैली में नहीं आई। साम्राज्य और सत्ता की प्राप्ति और उसकी ख़ातिर संघर्ष का मुसलमानों को कोई उपदेश नहीं दिया गया। इसके विपरीत पवित्र क़ुरआन में यह आया है कि हुकूमत और सत्ता सर्वोच्च अल्लाह का एक इनाम है। सर्वोच्च अल्लाह यह इनाम उन लोगों को देता है जो ईमान लाएँ, अच्छे कर्म करें। “अल्लाह ने उन लोगों से जिन्होंने ईमान को अपनाया और अच्छे कर्म किए, यह वादा किया है कि उनको ज़मीन में ख़िलाफ़त प्रदान करेगा।” (क़ुरान, 24:55) अत: शरीअत की सबसे पहली, सबसे मौलिक और अस्ल माँग इंसान से यह है कि वह ईमान लाए और भले कर्म करे। ईमान और भले कर्मों ही के बारे में क़ियामत के दिन पूछा जाएगा। ईमान और भले कर्म ही हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी हैं। जब मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों की संख्या उल्लेखनीय हद तक हो जाए जो ईमान और अच्छे कर्मों के गुणवाले हों तो फिर समाज में वह इस्लामी रंग पैदा होने लगता है जिसको पवित्र क़ुरआन ने अल्लाह का रंग क़रार दिया है। “अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंह हो सकता है? और हम तो उसी की बन्दगी करते हैं।” (क़ुरआन, 2:138) जिन ख़ूबियों को सर्वोच्च अल्लाह ने अपनाने का आदेश दिया है उनको अपनाओ और जिन बुराइयों से बचने का आदेश दिया है उनसे बचो, यही अर्थ है अल्लाह का रंग अपनाने के। जब यह कैफ़ियत प्राप्त होने लगती है तो फिर यह ज़रूरी हो जाता है कि समाज में अच्छाई की शक्तियों को बढ़ावा दिया जाए और बुराई की शक्तियों को दबाया जाए। अगर बुराई की शक्तियों को दबाने का समाज में कोई प्रबन्ध नहीं है तो फिर अच्छाई की शक्तियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अस्ल ज़मानत तो यह है कि मुस्लिम समाज में जनाधार इतना जागरूक हो, प्रशिक्षण और नैतिक आचरण का स्तर इतना उच्च हो कि उसके डर से कोई व्यक्ति खुलकर बुराई न कर सकता हो। और अगर कोई खुलकर बुराई करे तो मुस्लिम समाज उसपर इतनी सख़्त प्रतिक्रिया दे कि आगे से लोगों को इस प्रतिक्रिया के डर से बुराई का जुर्म करने की हिम्मत न हो।
सबसे पहला स्तर तो यह है जो बयान किया गया, लेकिन कभी-कभी इस सामाजिक दबाव से काम नहीं चलता। इस सामाजिक दबाव के बावजूद बहुत-से दुष्चरित्र लोग ऐसे होते हैं जो समाज में बुराई का जुर्म करना चाहते हैं और बुराई का जुर्म करने के लिए हर वक़्त तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों से निमटने के लिए राज्य की शक्ति दरकार होती है। इसलिए सर्वोच्च अल्लाह ने वादा किया है कि जब तुम इस सतह पर आ जाओगे कि तुम्हारा लक्ष्य सामाजिक नैतिकता और इस्लामी समाज की स्थापना हो जाए और ऐसे लोगों की उल्लेखनीय संख्या अस्तित्व में आ जाए जो इस्लामी नैतिकता पर कार्यरत रहते हैं और समाज में नैतिकता पर कार्यरत रहना चाहते हैं तो सर्वोच्च अल्लाह सत्ता की नेमत तुम्हें प्रदान करेगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह की तरफ़ से इनाम के तौर पर दिया जाएगा।
ख़िलाफ़त की धारणा
यहाँ पवित्र क़ुरआन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त किया है और यह पवित्र क़ुरआन की एक मौलिक शब्दावली है। لیستخلفنھم فی الارض (लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल-अर्ज़) का अर्थ है “सर्वोच्च अल्लाह उनको ज़मीन में ख़िलाफ़त प्रदान करेगा।” ख़िलाफ़त के शाब्दिक अर्थ उत्तराधिकार के आते हैं। यानी उत्तमकर्मी इंसानों को सर्वोच्च अल्लाह अपने उत्तराधिकार का सौभाग्य प्रदान करेगा। उत्तराधिकार कई तरह का होता है। आप किसी संस्था के प्रमुख हों और कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हों और जाने से पहले किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। यह उत्तराधिकार का एक प्रकार है। किसी संस्था का प्रमुख अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी जगह जो नया आदमी प्रमुख बनेगा वह मरनेवाले का उत्तराधिकारी हो जाएगा। यह दो तरह का उत्तराधिकार तो जाना-माना है। सर्वोच्च अल्लाह ने निश्चय ही इन अर्थों में इंसान को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। सर्वोच्च अल्लाह न ग़ैर-हाज़िर होता है, न उसपर मौत हावी होती है। वह तो हमेशा जीवित रहनेवाला है। ज़िन्दा और क़ायम रहनेवाला है। वह हर वक़्त, हर जगह मौजूद है। हर चीज़ उसके ज्ञान में है और उसके अधिकार में है। अत: उसके अनुपस्थित होने की भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उत्तराधिकार की इन दो के अलावा भी दो क़िस्में होती हैं। कभी-कभी उत्तराधिकार इंसान की आज़माइश के लिए होता है। और कभी-कभी उत्तराधिकार किसी को सम्मानित करने के लिए होता है। उदाहरणार्थ आपने कोई मदरसा बनाया है। वहाँ आप शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा देने के दौरान कोई विद्वान आ जाते हैं, जिनको आप इज़्ज़त देना चाहते हों तो आप अपनी जगह से उठकर कहते हैं कि आज आप दर्स दीजिए यानी पढ़ाइए। यह उत्तराधिकार मान-सम्मान का उत्तराधिकार होता है। आप मौजूद हैं। आपके सामने वह साहब क़ुरआन की शिक्षाएँ लोगों को बता रहे हैं और गोया आपके उत्तराधिकार की हैसियत से शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप मौजूद नहीं या दुनिया से चले गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनको इज़्ज़त देना चाहते हैं।
दूसरी शक्ल होती है आज़माइश और इम्तिहान की। वह यह कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसमें पचास छात्र हैं। पढ़ाते-पढ़ाते आपने कुछ छात्रों का ज्ञान जाँचने के लिए उनमें से किसी से कहा कि ज़रा आइए और सबके सामने आकर लेक्चर दीजिए। मैं भी अपनी क्लास में ऐसा करता हूँ। सामने छात्रों के साथ कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और एक विद्यार्थी से कहता हूँ कि आप क्लास लीजिए मैं देखता हूँ। यहाँ अस्ल में इम्तिहान लेना उद्देश्य होता है। तो गोया इम्तिहान और सम्मानित करना भी कभी-कभी इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। सर्वोच्च अल्लाह ने इंसानों को आज़माइश और सम्मानित करने के लिए उत्तराधिकारी बनाया है। सर्वोच्च अल्लाह इंसानों को आज़माकर शेष प्राणियों को यह दिखाना चाहता है कि जो प्रतिभाएँ सर्वोच्च अल्लाह ने इंसान में रखी थीं, उन प्रतिभाओं को उसने किस हद तक प्रयुक्त किया। वह किस हद तक अल्लाह के आदेशों के अनुसार चला। शरीअत ने उसपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं वे उसने किस हद तक पूरी की हैं। इस आज़माइश के साथ-साथ इंसान को सम्मानित करना भी अभीष्ट है। इसलिए इस्लाम का जो संवैधानिक या प्रशासनकि क़ानून है, उसका मौलिक बिन्दु ख़िलाफ़त और ख़िलाफ़त से सम्बन्धित चर्चाएँ हैं। पश्चिम में आजकल क़ानून की एक शब्दावली प्रचलित हुई है ग्रंडनार्म (grundnorm). ग्रंडनार्म जर्मन भाषा का शब्द है। इसका उर्दू अनुवाद है ‘अस्लुल-उसूल’। किसी व्यवस्था का जो ‘अस्लुल-उसूल’ होता है, व्यवस्था का मौलिक बिन्दु, जिसपर पूरी व्यवस्था खड़ी हुई हो। जैसे वृक्ष का बीज होता है। इसको ‘अस्लुल-उसूल’ या ग्रंडनार्म कहते हैं। इसी तरह पूरी राजनैतिक और संवैधानिक व्यवस्था के बीज और ‘अस्लुल-उसूल’ को जर्मन भाषा में ग्रंडनार्म कहते हैं। यह शब्दावली अंग्रेज़ी में भी प्रयुक्त होती है।
सर्वोच्च अल्लाह की ‘हाकिमियत’
इस्लाम के संवैधानिक और प्रशासनकि क़ानून का ग्रंडनार्म सर्वोच्च अल्लाह की हाकिमियते-मुतलक़ा (पूर्ण प्रभुत्व) का उसूल और इंसान की ख़िलाफ़त और उत्तराधिकार की धारणा है। कायनात का वास्तविक मालिक और वास्तविक शासक केवल सर्वोच्च अल्लाह है। जो मालिक होगा वही अधिकारी भी होगा। यह बहस कल भी हुई थी। जो वास्तविक अधिकारी होगा वह हर तरह से अधिकारी होगा। जो पूर्ण मालिक होगा वह अधिकारी भी होगा। चूँकि सर्वोच्च अल्लाह स्रष्टा है, इसलिए मालिक है और चूँकि वह स्रष्टा और मालिक है इसलिए अधिकारी भी है। इसलिए शासन करने का, सत्ता को प्रयोग करने का, क़ानून और व्यवस्था देने का, अच्छे और बुरे का फ़ैसला करने का अन्तिम और वास्तविक अधिकार भी सर्वोच्च अल्लाह ही को है। यह वह चीज़ है जिसको आजकल की शब्दावली में soveriegnty कहते हैं। अंग्रेज़ी में जिन लेखकों ने इस्लाम की संवैधानिक व्यवस्था पर लिखा है वे इसको divine sovriegnty के शब्द से याद करते हैं यानी सर्वोच्च अल्लाह की हाकिमियते-मुतलक़ (पूर्ण प्रभुत्व), हाकिमियते-इलाहिया, या सर्वोच्च अल्लाह का इक़तिदारे-आला।
इस कायनात में सर्वोच्च अल्लाह की पूर्ण सत्ता दो तरह से ज़ाहिर होती है। एक तो उस आदेश के ज़रीये ज़ाहिर होती है जिसको हुक्मे-तकवीनी (प्राकृतिक नियम) कहते हैं। इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है। यानी सर्वोच्च अल्लाह के जारी किए हुए वे स्वाभाविक एवं भौतिक और ग़ैर-तशरीअई आदेश जिनका पालन करने पर हर प्राणी बिना ना-नुकुर किए मजबूर है। ये वे आदेश हैं जिनको ‘सुनने-इलाहिया’ भी कहा जाता है। इन आदेशों में कोई भी सर्वोच्च अल्लाह की ना-फ़रमानी नहीं कर सकता और आरम्भ से उन आदेशों पर आज्ञाकारिता से अमल हो रहा है। सर्वोच्च अल्लाह की हर सृष्टि, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, ग्रह और उपग्रह, इंसान और जानवर, फ़रिश्ते और जिन्नात, परिंदे और दरिंदे, हर चीज़ और सृष्टि इन आदेशों की पैरवी कर रही हैं। उनको ‘अहकामे-तकवीनी’ (प्राकृतिक नियम) कहा जाता है। “और सूर्य अपने नियत ठिकाने के लिए चला जा रहा है। यह बाँधा हुआ हिसाब है प्रभुत्वशाली, ज्ञानवान का।” (क़ुरआन, 36:38) सूरज अल्लाह की रचना है। जिस रास्ते पर चला दिया है उसपर लाखों वर्ष से चल रहा है। इसी तरह से जिस रचना को जो भी आदेश दे दिया गया है वह उसके अनुसार कर रही है। इंसान भी ‘अहकामे-तकवीनी’ का इसी तरह पाबन्द है जिस तरह दूसरी रचनाएँ पाबन्द हैं। ‘हुक्मे-तकवीनी’ के पालन में कोई इंसान ज़र्रा बराबर इधर-उधर नहीं कर सकता। इसपर पाबन्द है कि कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ मरना है। इसमें एक क्षण की देर हो सकती है न पहले यह हो सकता है। ये ‘हुक्मे-तकवीनी’ है। इंसान जीवन में क्या करेगा यह अल्लाह को मालूम है। बहुत-से मामलात में इंसान पाबन्द है। उसको ख़ूबसूरत बनाया है कि बदसूरत बनाया है। किसी इंसान को अफ़्रीक़ा में पैदा क्या या एशिया में, या कालों में पैदा किया या गोरों में पैदा किया है। कोई यह नहीं पूछ सकता कि मुझे अमुक का बेटा क्यों बनाया, अमुक का क्यों नहीं बनाया। यह सब ‘अहकामे-तकवीनी’ हैं जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें न हम कुछ कर सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे अमुक की बहन या भाई क्यों बनाया और अमुक की बहन क्यों नहीं बनाया। यह ‘हुक्मे-तकवीनी’ कहलाता है। सर्वोच्च अल्लाह की हाकिमियते-मुतलक़ उसके तकवीनी आदेशों के ज़रिये कायनात के कोने-कोने में पूर्ण रूप से जारी है। ‘अहकामे-तकवीनी’ के विपरीत, सर्वोच्च अल्लाह के आदेशों का एक सीमित हिस्सा ‘अहकामे-तशरीई’ या शरई आदेश कहलाता है। आदेशों का यह प्रकार केवल इंसानों और जिन्नात के लिए है। ‘अहकामे-तशरीई’ का पालन करने या न करने की इंसानों को आज़ादी दे दी गई है कि वे चाहें तो उन आदेशों की पैरवी करके दुनिया और आख़िरत की सफलता प्राप्त कर लें। और न करना चाहें तो आख़िरत के शाश्वत दंड के लिए तैयार रहें। ‘अहकामे-तशरीई’ इस इम्तिहान और आज़माइश का एक ज़रिया और निशानी हैं जिसकी ख़ातिर इंसान को पैदा किया गया है। चुनाँचे अपने आदेशों में सर्वोच्च अल्लाह ने एक थोड़ा-सा हिस्सा, जो बहुत-सीमित है, ऐसा रखा है जहाँ इंसान को आज़ादी दी गई है। इंसान चाहे तो अल्लाह के आदेशों पर अमल करे और चाहे तो न करे। चाहे तो नमाज़ पढ़े और न चाहे तो न पढ़े। ज़कात दे या न दे। अल्लाह की शरीअत पर अमल करे या न करे। यह आज़ादी स्वयं अल्लाह ने दी है। इसलिए कि इस सीमित दायरे में सर्वोच्च अल्लाह आज़माइश करके दिखाना चाहता है कि कौन पैरवी करता है और कौन नहीं करता।
आज़माइश उसी समय हो सकती है जब आज़ादी हो। अगर आप बच्चों को परीक्षा कक्ष में बिठा दें और उनपर सवालात के विशेष उत्तर देने ही की पाबन्दी हो तो यह इम्तिहान नहीं कहलाएगा। यह इम्तिहान तब होगा जब छात्रों को सवाल का सही या ग़लत हर तरह का जवाब देने की आज़ादी हो। उनको यह भी आज़ादी हो कि चाहें तो उत्तर लिखनेवाली कापी पर कुछ लिखें और न चाहें तो कुछ न लिखें। इम्तिहान के दौरान जब तक पूरी आज़ादी न होगी उस समय तक इम्तिहान नहीं होगा। इसलिए सर्वोच्च अल्लाह ने साठ-सत्तर वर्ष के इस सीमित समय के लिए हर इंसान को आज़ादी दी है और इसी में आज़माइश करना उद्देश्य है। आज़माइश के लिए ज़रूरी होता है कि आज़माइश के लिए जीवन के अखाड़े में उतरनेवाला उन सीमाओं का पाबन्द हो जो आज़माइश करनेवाले ने लागू की हैं। अगर इन सीमाओं से बाहर जाएगा तो आज़माइश में नाकाम रहेगा और अगर सीमाओं के अन्दर रहेगा तो सफल हो जाएगा। इसलिए आज़माइश और अल्लाह के उत्तराधिकार की अनिवार्य अपेक्षा है कि इंसान इन नियमों का पालन करे जिनके पालन का वास्तविक स्वामी ने आदेश दिया है। शब्द ‘ख़िलाफ़त’ से भी यही ज़ाहिर होता है। और यही ख़िलाफ़त की तार्किक अपेक्षा है। इंसान की हैसियत की अनिवार्य निशानी भी है और सर्वोच्च अल्लाह के सृष्टि के रचयिता होने का एक तक़ाज़ा भी है। यही वजह है कि पवित्र क़ुरआन में कुछ आदेशों के उल्लंघन पर सर्वोच्च अल्लाह की तरफ़ से जंग का एलान किया गया है कि अगर अमुक-अमुक काम नहीं करोगे, या अमुक और अमुक जुर्म करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से एलाने-जंग सुन लो, इसलिए कि तुम्हारा कार्य-क्षेत्र सीमित था। तुम जिस कार्य-क्षेत्र में रहने के पाबन्द थे, उसका तुमने उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के बाद तुमने उस mandate को समाप्त कर दिया जो तुम्हें प्रदान किया गया था। मेंडेट के लिए ज़रूरी है कि उन नियमों का पालन किया जाए जिनके तहत मेंडेट प्रदान किया गया है। अत: जब मेंडेट को तोड़ा जाएगा और अल्लाह की ओर से निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया जाएगा तो सर्वोच्च अल्लाह की तरफ़ से जो मान-सम्मान ख़िलाफ़त के रूप में प्रदान किया गया था वह समाप्त हो जाएगा। वह सम्मान वापस ले लिया जाएगा और सम्मान समाप्त कर दिया जाएगा। जब मान-सम्मान समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर दोस्त और दुश्मन में अन्तर नहीं रहेगा। दोस्त भी दुश्मन क़रार पाएगा। जब दोस्त दुश्मन क़रार पाएगा तो एलाने-जंग दुश्मन के ख़िलाफ़ होता है दोस्त के ख़िलाफ़ नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने एलाने-जंग किया।
इस्लामी राज्य के मौलिक कर्तव्य
ये वे कारण हैं जिनके लिए पवित्र क़ुरआन ने कुछ मार्गदर्शन ऐसे दिये हैं कि जिनका निर्वहन उन मुसलमानों को करना चाहिए जिनको सर्वोच्च अल्लाह ने ज़मीन में सत्ता प्रदान की है। पवित्र क़ुरआन की प्रसिद्ध आयत है, यानी सूरा हज की इकतालीसवीं आयत जिसमें कहा गया है। “वे लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में सत्ता प्रदान करें तो नमाज़ का आयोजन करें और ज़कात दें और भलाई का आदेश दें और बुराई से रोकें, और अल्लाह ही के क़ब्ज़े में सब कामों का अंजाम है।” (क़ुरआन, 22:41)
इस आयत के एक-एक शब्द पर ग़ौर कीजिए। “अगर हम उन्हें ज़मीन में सत्ता प्रदान करें।” यह नहीं कहा गया कि “जब हम उन्हें ज़मीन में सत्ता दें”। इसलिए कि हो सकता है कि किसी को सत्ता और हुकूमत का यह सम्मान मिले, किसी को न मिले। किसी को सर्वोच्च अल्लाह इस प्रतिदान से विभूषित करे किसी को न करे। यह तो उसकी मर्ज़ी है। अगर वह तुम्हें सत्ता की नेमत प्रदान करे तो फिर तुम्हें ये चार काम करने होंगे। इन दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ें कि एक तरफ़ ख़िलाफ़त का इनाम है जिसका वादा किया गया है। दूसरी तरफ़ शर्त है कि अगर सर्वोच्च अल्लाह तुम्हें सत्ता दे तो फिर यह काम तुम्हें करने हैं। दोनों से पता चलता है कि इंसान का यह ‘हक़’ नहीं है कि उसको हुकूमत मिले। इंसान का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सत्ता और शासन के लिए कोशिश करे। जिस चीज़ के लिए उसे कोशिश करनी है वह केवल अल्लाह की प्रसन्नता है। इंसान को जिस चीज़ के लिए काम करना है वह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शरीअत के आदेशों के लिए करना है। इस्लामी समाज में नैतिक प्रवृत्तियों के फैलाव के लिए काम करना है। जब सर्वोच्च अल्लाह हुकूमत और सत्ता का इनाम प्रदान करे तो फिर उसको ये चार काम भी करने चाहिएँ। नमाज़ क़ायम करे, ज़कात दे, अच्छाइयों का आदेश दे और बुराइयों से रोके। ये चार कर्तव्य इस्लामी राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं। इनके अलावा भी अनेक कर्तव्य हैं, लेकिन ये चार कर्तव्य मौलिक कर्तव्य हैं जो वस्तुतः शीर्षक हैं और चार प्रकार के कर्तव्यों की निशानदेही करते हैं।
नमाज़ के बारे में हर मुसलमान जानता है कि यह इस्लाम की सबसे सर्वप्रथम और आख़िरी इबादत है। शेष तमाम इबादतों से इंसान कुछ परिस्थितियों में छूट सकता है, लेकिन नमाज़ से आख़िरी दम तक छुट्टी नहीं पा सकता। अगर हिलने-जुलने की ताक़त नहीं और मुख तक नहीं हिला सकता तो दिल में सोचे कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ। जब तक दिल और दिमाग़ काम कर रहे हैं नमाज़ से छुट्टी नहीं है। यह वह इबादत है जो सबसे पहली भी है और सबसे आख़िरी भी है। लेकिन इस इबादत का एक सामूहिक महत्व भी है। याद कीजिए कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दुनिया से गए और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) सक़ीफ़ा-बनी-साअदा में में इकट्ठे हुए, वहाँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के उत्तराधिकार के लिए विभिन्न नाम पेश हो रहे थे। बड़े-से-बड़े सहाबा के नाम विचाराधीन थे। लेकिन जिस महानतम और उच्च कोटि के व्यक्तित्व के नाम पर तमाम प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने सर्वसहमति व्यक्त की वे हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे। उनके चयन के लिए प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने जो तर्क दिया वह यह था कि जिनके अद्वितीय व्यक्तित्व को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमारी नमाज़ की इमामत के लिए उचित क़रार दिया वे हमारी दुनिया के मामलों में भी नेतृत्व के लिए सबसे उचित होंगे। गोया उन्होंने नमाज़ और व्यावहारिक जीवन को एक-दूसरे के जैसा समझा था। कल आप में से किसी ने कहा था कि ‘क़ियास’ का एक और उदाहरण दें। यह ‘क़ियास’ का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सामूहिक इबादत के लिए जिस व्यक्तित्व का चयन किया, उसी व्यक्तित्व का चयन मुसलमानों के सामूहिक जीवन के नेतृत्व के लिए भी होना चाहिए। इससे पता चला कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के नज़दीक नमाज़ और मुसलमानों की राजनैतिक जीवन में बड़ी गहरी समानताएँ पाई जाती हैं। मुसलमानों का राजनैतिक और सामूहिक जीवन नमाज़ की तरह होना चाहिए।
नमाज़ में एक आध्यात्मिक माहौल होता है। मुस्लिम समाज में भी एक आध्यात्मिक माहौल कार्यरत होना चाहिए। नमाज़ में अल्लाह का डर नमाज़ियों पर छाया होता है। मुस्लिम समाज में भी सब पर अल्लाह का डर छाया होना चाहिए। नमाज़ के दौरान कोई व्यक्ति अपने भौतिक हितों की ज़्यादा परवाह नहीं करता, सिवाय यह कि कोई बड़ा भौतिक लाभ हो। मुस्लिम समाज में लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। नमाज़ में अनुशासन का पूरा पालन होता है। मुस्लिम समाज में भी ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमानों का नेतृत्व नमाज़ में वह व्यक्ति करता है जो उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सामूहिक नेतृत्व भी ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमानों की नमाज़ का इमाम मुसलमानों के नेतृत्व का उस समय तक हक़दार है जब तक वह शरीअत के अनुसार नेतृत्व कर रहा हो। जब वह ग़लती करे तो हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि उसे टोक दे। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) भी नमाज़ पढ़ा रहे हों। इमाम मुस्लिम (रह॰) भी नमाज़ पढ़ा रहे हों और नमाज़ पढ़ाने के दौरान तिलावत में कोई ग़लती कर गुज़रें तो मेरे जैसे गुनाहगार इंसान को भी न केवल ‘हक़’ है, बल्कि यह मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनको इस ग़लती पर टोक दूँ और उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस ग़लती को दुरुस्त करें। इसमें छोटे और बड़े का कोई अन्तर नहीं। छोटे-से-छोटा मुक़तदी (इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नेवाला) भी ग़लती की निशानदेही करेगा तो बड़े-से-बड़े इमाम की ज़िम्मेदारी है कि ग़लती को दुरुस्त करे। बड़े-से-बड़े आदमी की ज़िम्मेदारी है कि तुरन्त अपनी ग़लती को स्वीकार करे और ठीक करे यहाँ तक कि पैग़ंबर की भी ज़िम्मेदारी है कि नमाज़ में अगर इनसानी कमज़ोरी के कारण कोई भूल-चूक हो जाए तो जैसे ही ध्यान दिलाया जाए तो उस ग़लती को ठीक करे। आपने ‘ज़ुल-यदैन’ की हदीस पढ़ी होगी। यहाँ उसे पेश किया जा रहा है—
अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) (ज़ुह्र या अस्र की) दो रकअत पढ़कर (मुक़्तदियों की तरफ़) पलटे तो ज़ुल-यदैन ने आपसे पूछा, “अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं?” तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा, “क्या ज़ुल-यदैन सच कह रहे हैं?” लोगों ने कहा, “हाँ! (आपने दो रकअत ही पढ़ी हैं) तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) खड़े हुए और आख़िरी दो रकअतें पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर अल्लाहु अकबर कहा, फिर अपने पहले सजदे की तरह या उससे कुछ लम्बा सजदा किया, फिर अल्लाहु अकबर कहा और सिर उठाया, फिर अपने उसी सजदे की तरह या उससे कुछ लम्बा सजदा किया।” (सुनन तिरमिज़ी, हदीस:399)
इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने चार रकअत की नमाज़ भूल से दो रकअत पर ही समाप्त कर दी थी, मगर ज़ुल-यदैन के याद दिलाने पर आपने उसे पूरा किया। इससे साबित होता है कि इमाम कोई भी हो उसकी ग़लती पर उसे टोका जा सकता है। तो जिस तरह से नमाज़ में हर व्यक्ति अपने क़ाइद और इमाम की ग़लती को ठीक करने का पाबन्द है, उसी तरह सामूहिक जीवन में हर व्यक्ति पाबन्द है। जिस तरह इमाम पाबन्द है कि ग़लती को दुरुस्त करे, इसी तरह सामूहिक जीवन में भी इमाम और लीडर के लिए ज़रूरी है कि ग़लती को दुरुस्त करे। अगर इमाम इमामत के योग्य न रहे, उदाहरण के रूप में इसका वुज़ू टूट गया तो उसको उसी लम्हे इमामत से अलग हो जाना चाहिए। उसी पल अलग होना चाहिए और उसी पल किसी दूसरे आदमी को इमाम की जगह लेनी चाहिए। सामूहिक जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। इमाम और मुक़्तदी का रुख़ एक ही तरफ़ यानी क़िबले की तरफ़ होता है। सामूहिक जीवन में भी इमाम और आम लोगों का रुख़ एक ही तरफ़ होना चाहिए। इस तरह से आप ग़ौर करें तो इन कुछ उदाहरणों के अलावा भी, जो मैंने यह बताने के लिए दिए हैं कि नमाज़ और सामूहिक जीवन में बड़ी गहरी समानता है। नमाज़ और मुसलमानों के राजनैतिक और सामूहिक जीवन में बहुत-सी गहरी समानताएँ पाई जाती हैं। जब पवित्र क़ुरआन यह कहता है कि मुसलमानों को जब सत्ता मिले तो वह सबसे पहले नमाज़ क़ायम करें। तो गोया पवित्र क़ुरआन यह याद दिलाना चाहता है कि वह हुकूमत का काम संभालने के बाद सबसे पहले न केवल नमाज़ की व्यवस्था विधिवत रूप से क़ायम करें, बल्कि सबसे पहले इस बात को निश्चित बनाएँ कि उनका सामूहिक जीवन भी नमाज़ की स्पिरिट के अनुसार हो।
इससे एक और बात भी पता चली। वह यह कि नमाज़ क़ायम करने का यह निर्देश शासकों के लिए है। इसका अर्थ यह है कि शासक स्वयं नमाज़ पढ़नेवाले हों। नमाज़ और उसके आदेश, उसके मसाइल (समस्याओं) और उसकी मूलात्मा के बारे में जानते हों, नमाज़ पढ़ा सकते हों। जब तक ऐसा नहीं होता और लीडर नमाज़ नहीं पढ़ा सकता तो वह सत्ता में आकर क्या ख़ाक नमाज़ क़ायम करेगा। अगर लीडर ऐसा हो कि सजदे में जाकर साथ में खड़े मुक़्तदी से पूछे कि What’s next तो वह क्या नमाज़ क़ायम करेगा? भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रसिद्ध राजनैतिक लीडर के बारे में सुना है कि जब वे राजनैतिक पद पर आसीन हुए तो किसी ऐसे इलाक़े में उनको जाना हुआ जहाँ उनको मजबूरन कोई नमाज़ पढ़नी पड़ी। पहले कभी इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ था इसलिए पहले तो बहाना किया कि मुझे तो नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता। तो जो आदमी साथ लेकर जा रहा था, उसने कहा कि बस जनाब आप ख़ामोशी से वह कुछ करते रहें जो मैं करूँगा, ज़बान से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। चुनाँचे यह लीडर साहब नमाज़ के लिए चले गए और नमाज़ के दौरान कनखियों से हम-राही को देखते रहे कि क्या कर रहे हैं। स्वयं भी इसी तरह करते रहे। लेकिन जब सजदे में गए तो परेशान हो गए तो साथी की तरफ़ मुँह करके कहने लगे कि What next? (आगे क्या करूँ?) ज़ाहिर है कि जब ऐसा आदमी मुसलमानों का लीडर होगा तो वह नमाज़ क़ायम करने का कर्तव्य नहीं निभा सकेगा। दूसरा कर्तव्य यह है कि सत्ता में आने के बाद ज़कात अदा करने का प्रबन्ध करें। ज़कात भी एक इबादत है। लेकिन जिस तरह नमाज़ में बहुत-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं उसी तरह ज़कात में भी बहुत-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं। पवित्र क़ुरआन ने ज़कात के तीन उद्देश्य बयान किए हैं। एक उद्देश्य ‘तज़किया-ए-माल’ (धन को शुद्ध करना) और ‘तज़किया-ए-मुआशरा’ (समाज-सुधार) है। इस्लामी समाज में माल हलाल और पाक होना चाहिए। जो माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए वह पूरी तरह हलाल माल होना चाहिए। यानी हर इंसान के पास जो धन-दौलत और सम्पत्ति है वह अत्यन्त पाक-साफ़, जायज़ और हलाल कमाई की होनी चाहिए। इस में हराम और नापाक तत्वों की मिलावट न हो। यह मुस्लिम समाज और मुस्लिम राज्य में माल की कैफ़ियत होनी चाहिए।
ज़कात और उससे मिलते-जुलते दूसरे आदेशों का दूसरा उद्देश्य यह है कि “ताकि वह (धन-दौलत) तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न लगाता रहे।” (क़ुरआन, 59:7) बल्कि पूरे समाज में चक्कर लगाता रहे। इस आयत पर विस्तार से आगे चलकर एक अलग ख़ुतबे में बात होगी।
ज़कात का तीसरा उद्देश्य यह है कि समाज में ऐसे ग़रीब और मसाकीन (दरिद्र) न रहें जो अपनी आवश्यकता को स्वयं भी पूरा न कर सकते हों और कोई और भी उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए मौजूद न हो। कमज़ोर और अपंग लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं के पूरे किए जाने की एक स्वचालित व्यवस्था मौजूद हो। अगर मुस्लिम समाज में ये तीनों काम हो रहे हों, तो उनका राज्य एक इस्लामी राज्य है।
इसके बाद कहा गया कि “वे अच्छाई का आदेश देंगे।” ‘अल-मारूफ़’ से मुराद वह अच्छाई और ख़ूबी है जिसको पवित्र क़ुरआन ने ख़ूबी स्वीकार क्या हो या इंसान की सद्बुद्धि उसको ख़ूबी और सद्गुण स्वीकार करती हो। हर वह गुण जिसको इंसान की सद्बुद्धि गुण मानती हो और वह शरीअत के आम सिद्धान्तों के अनुसार हो, वह ‘मारूफ़’ है। चुनाँचे क़ियामत आने तक हर वह अच्छाई और ख़ूबी जिसको किसी क्षेत्र के सदाचारी इंसान ख़ूबी क़रार दें और अच्छाई समझें, वह शरीअत के अनुसार भी हो और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शरीअत के उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हो तो वह ‘मारूफ़’ है और उसकी स्थापना इस्लाम के उद्देश्यों में से है। उसको बढ़ावा देना और परवान चढ़ाना इस्लामी राज्य की ज़िम्मेदारी है।
आख़िरी चीज़ है “वे मुनकर (बुराई) से रोकेंगे।” ‘मुनकर’ से मुराद हर वह बुराई है जिसको स्वीकार करने से इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति झिझकती हो। जिसे एक समझदार और नेक इंसान की तबीअत स्वीकार न करे और उसको बुरा समझे तो वह ‘मुनकर’ है। ‘मुनकर’ से मुराद वह बुराई भी है कि जिसको कोई भी सदाचारी इंसान देखे तो उसका इनकार करे। ‘मुनकर’ का शाब्दिक अर्थ है ‘वह जिसका इनकार किया जाए’। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी बुराई विचारणीय होती है या उसके बारे में लोगों के विभिन्न मत होते है, या जिनमें बुराई का पहलू सीमित और दबा हुआ होता है। ऐसी चीज़ों के इनकार पर मतभेद हो सकता है। कुछ लोग इनकार करते हैं और कुछ स्वीकार करते हैं। किसी का स्वभाव उसको पसन्द करता है किसी का नहीं करता। यह ‘मुनकर’ नहीं है। जिस चीज़ में मुसलमानों के दरमियान मतभेद हो वह ‘मुनकर’ नहीं है उसपर ‘नकीर’ नहीं की जाएगी। ‘नकीर’ का अर्थ है public condemnation. मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि जब ‘मुनकर’ का जुर्म हो रहा हो तो जहाँ तक सम्भव हो उसपर नकीर यानी आपत्ति करे, और जिस हद तक उसके लिए सम्भव है उससे ख़ुद को अलग रखे। लेकिन यह उसी समय होगा जब वह वाक़ई ‘मुनकर’ हो और हर इंसान की स्वाभाविक प्रकृति उसका इनकार करती हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसमें मतभेद पाया जाता हो। कुछ मुसलमान उसको स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ के विचार में उसको गवारा किया जा सकता हो और कुछ के ख़याल में नहीं किया जा सकता हो। ऐसी चीज़ को ‘मुनकर’ नहीं कहा जाएगा।
एक और चीज़ भी याद रखने की है जिससे कभी-कभी भ्रम होता है। कुछ चीज़ें शरीअत ने मुरव्वत (रिआयत) के ख़िलाफ़ समझी हैं और एक ऐसा इंसान जो परहेज़गार और निष्ठावान हो, ईशपरायण और निष्ठा के एक विशेष स्तर पर हो तो उसको यह शोभा नहीं देता कि वह काम करे। लेकिन अगर आम मुसलमान वह काम करता है तो कोई हरज नहीं। मान लीजिए कि इस्लामाबाद में खेल-कूद का कोई मेला हो रहा हो। वह एक गम्भीरता रहित चीज़ है। अगर आम इंसान वहाँ जाएँगे तो कोई बयान नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति किसी के जाने का नोटिस लेगा, इसलिए कि ऐसी चीज़ें शरीअत में पूरी तरह हराम या निषिद्ध नहीं हैं। लेकिन अगर कोई गौरवशाली और ऐसा व्यक्ति जिसको लोग दीन में नमूना समझते हों, इस तरह की गतिविधि में हिस्सा ले तो ठीक नहीं है। इसलिए उनके लिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। अगर आम लोग जाना चाहें तो जाएँ। यह ‘मुनकर’ नहीं होगा। आप डंडा लेकर लोगों को वहाँ जाने से रोकें तो यह ठीक नहीं। इसलिए कि हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति उसको नापसन्द नहीं करती। कभी-कभी हो सकता है कि एक चीज़ जायज़ हो, लेकिन नैतिक आचरण के स्तर या शिष्टाचार के ख़िलाफ़ हो। जितने ऊँचे नैतिक स्तर पर उसको होना चाहिए उससे नीचे हो, लेकिन जायज़ हो वह ‘मुनकर’ नहीं समझी जाएगी। इसलिए ‘मुनकर’ को समझने के लिए मौलिक चीज़ यह है कि ‘मुनकर’ वह है कि जो इंसान की स्वाभाविक प्रकृति के लिए स्वीकार्य न हो और शरीअत के बताए हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति पहुँचाती हो।
ये चार वे उद्देश्य हैं जिनको पवित्र क़ुरआन ने बयान किया है, ये इस्लामी राज्य के मौलिक उद्देश्यों में से हैं। इनके अलावा इस्लामी राज्य की और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जिनको आगे बयान किया जाएगा। लेकिन ये चार पवित्र क़ुरआन की उपर्युक्त आयत में आए हैं।
मुस्लिम समाज का गठन : इस्लाम का सर्वप्रथम लक्ष्य
राज्य के बारे में तमाम इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने लिखा है कि यह इस्लाम का मूल उद्देश्य नहीं, बल्कि द्वितीय उद्देश्य है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अभीष्ट के दो प्रकार बयान किए हैं। एक वह जो मूल उद्देश्य हो। जैसे नमाज़ वास्तविक उद्देश्य है। यह किसी और उद्देश्य की प्राप्ति का ज़रिया नहीं, बल्कि स्वयं एक उद्देश्य है। शरीअत ने प्रत्यक्ष रूप से नमाज़ का आदेश दिया है, लेकिन वुज़ू प्रत्यक्ष रूप से अभीष्ट नहीं है, नमाज़ के लिए ज़रूरी है। अगर नमाज़ का समय नहीं है और नमाज़ पढ़ने की नीयत नहीं तो फिर वुज़ू ज़रूरी नहीं है। वुज़ू की फ़र्ज़ियत (अनिवार्यता) मूल उद्देश्य नहीं, बल्कि वसीले के तौर पर है। नमाज़ की फ़र्ज़ियत अभीष्ट के तौर पर है। इसी तरह से राज्य की फ़र्ज़ियत अभीष्ट नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जिसके बिना बहुत-से इस्लामी आदेशों पर कार्यान्वयन नहीं हो सकता। जिसके बिना मुस्लिम समाज की रक्षा नहीं की जा सकती। जिसके बिना मुस्लिम समाज के नैतिक मूल्यों को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मूल उद्देश्य मुस्लिम समाज और मुस्लिम उम्मत है। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने उम्मत की स्थापना की दुआ की थी, राज्य की स्थापना की दुआ नहीं की थी। यह नहीं कहा था कि “ऐ अल्लाह! मेरी सन्तान में लोगों को बादशाह बना दे और साम्राज्य प्रदान कर दे।” यह कहा था कि “अपना आज्ञाकारी समुदाय बना...” (क़ुरआन, 2:128) और जब पवित्र क़ुरआन ने मुसलमानों को सामूहिक ज़िम्मेदारी दी तो यह कहा कि “तुम उत्तम समुदाय हो जो लोगों (के मार्गदर्शन) के लिए निकाले गए हो, तुम भलाई का आदेश देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।” (क़ुरआन, 3:110) अत: मूल उद्देश्य उम्मत का गठन एवं प्रशिक्षण है। लेकिन राज्य की शक्ति भी उम्मत (मुस्लिम समुदाय) के लिए दरकार है। उम्मत की सहायता के लिए राज्य की ताक़त मौजूद होगी तो उम्मत को काम करने में आसानी होगी। उम्मत के बहुत-से काम आसान हो जाएँगे अगर राज्य की सहायता प्राप्त हो। उम्मत की रक्षा आसान होगी कि अगर राज्य उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद हो। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक जगह फ़रमाया। कुछ लोगों का कहना है कि यह कथन हज़रत उसमान ग़नी का है। कुछ लोगों
का कहना है कि हदीस है। लेकिन बहरहाल हदीस की किताबों में आया है और इस्लाम के एक मौलिक सिद्धान्त को बताता है। फ़रमाया कि “इस्लाम एक आधार है। और हुकूमत की हैसियत एक चौकीदार की है। जिस इमारत का कोई आधार न हो वह गिर जाएगी। और जिस इमारत का कोई चौकीदार न हो वह नष्ट हो जाती है और लूट ली जाती है।” मानो मानव-जीवन एक इमारत है। इस इमारत का आधार इस्लाम से जुड़ाव है। या गोया मुस्लिम समाज एक इमारत है। इस इमारत का आधार शरीअत और दीन की शिक्षाओं पर है। सुल्तान और हुकूमत उसकी निगहबान और रक्षक है।
राज्य की आवश्यकता
यह बात कि राज्य की स्थापना मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए ज़रूरी है, पहले दिन से ही अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रोग्राम में शामिल थी। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ पश्चिमी लेखकों ने यह लिखा है और उनकी देखा-देखी बहुत-से मुसलमानों ने भी यह बात कहनी शुरू कर दी है। हालाँकि यह बात बड़ा दुस्साहस और गुस्ताख़ी की मालूम होती है, बल्कि शायद काफ़िराना प्रकार की बात है। एक प्राच्यविद् के बारे में प्रसिद्ध है कि इस्लाम का बड़ा हमदर्द है। इस्लाम के इन हमदर्द साहब डब्ल्यू मंटगमरी वाट (W. Montgomery Watt) ने लिखा है। यह एक अंग्रेज़ था और कुछ वर्ष पहले उसका देहान्त हो गया है। सीरत (नबी सल्ल. की जीवनी) उसका विषय था और उसने सीरत पर कई किताबें लिखी हैं। उसकी दो प्रसिद्ध किताबें हैं Muhammad at Mecca और Muhammad at Madina उसने पूरी किताबों में अपने पाठकों को जो बात ज़ेहन में बिठाई है वह यह है कि मक्का में इस्लाम कुछ और था और मदीना में इस्लाम कुछ और था। मक्का में तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों को केवल नैतिक आचरण सिखाना चाहते थे, अच्छा मुसलमान बनाना चाहते थे। और दीने-इबराहीमी के बारे में उनका जो तसव्वुर था वह अरब के लोगों को उसके अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन जब सत्ता मिली और मदीना में जाकर ताक़त प्राप्त हो गई तो आपने मक्का के दौर के आईडियल और मापदंड छोड़ दिए, हुकूमत और सत्ता के रास्ते पर चल पड़े, एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। यह उसकी दोनों किताबों का सार है है। यह बात कुछ मुसलमानों ने भी लिखी है। यह बात बिलकुल सुबूतों और घटनाओं की दृष्टि से ग़लत है।
पवित्र क़ुरआन में मक्की सूरतों में अनगिनत आयतें हैं जिनमें यह बताया गया है कि नेक अमल और ईमान के परिणामस्वरूप सर्वोच्च अल्लाह सत्ता का सौभाग्य और ज़िम्मेदारी प्रदान करता है। मक्का मुकर्रमा में अवतरित होनेवाली अनेक आयतों और सूरतों में ख़िलाफ़त का ज़िक्र है। हिजरत से पहले जो आयतें अवतरित हुईं उनमें कहा गया कि “ऐ अल्लाह! किसी ऐसी हुकूमत को मेरा मददगार बना दे जो इस काम में मेरी मददगार हो।” (क़ुरआन, 17:80) अतीत में जितने पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) गुज़रे हैं, जिनमें से कई एक का ज़िक्र पवित्र क़ुरआन में भी आया है, उनमें से अनेकों को सर्वोच्च अल्लाह ने हुकूमत प्रदान की। उनके पूरे विवरण से मक्की दौर की सूरतें भरी हुई हैं। उनके बारे में पवित्र क़ुरआन ने बताया कि “ये हैं जिनको अल्लाह ने मार्गदर्शन दिया तो तुम इन (अंबिया) की राह पर चलो।” (क़ुरआन, 6:90) तो अगर पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) के जीवन की पैरवी करनी है तो उनमें हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) भी हैं, हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम), हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम), हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत यूशअ (अलैहिस्सलाम), ये सब वे थे जिनको सर्वोच्च अल्लाह ने सत्ता और अधिकार प्रदान किया। अत: सत्ता और अधिकार की आवश्यकता और मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए उसका अनिवार्य होना मक्की सूरतों में जगह-जगह, कहीं-कहीं इशारे के रूप में मौजूद है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब आरम्भिक दौर में इस्लाम की ओर बुलाया करते थे। सीरत इब्ने-हिशाम और सीरत (मुहम्मद सल्ल. की जीवनी) और हदीस की अधिकतर किताबों में इसके विवरण मौजूद हैं। इन विवरणों में आया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अरब के क़बीलों की विभिन्न सभाओं में जाया करते थे और फ़रमाया करते थे कि मैं जिस चीज़ की दावत दे रहा हूँ उसको अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो सर्वोच्च अल्लाह अरब और अजम के ख़ज़ाने आपपर खोल देगा। यह बात आपने कई बार फ़रमाई। जब आपके चाचा अबू-तालिब के पास मक्का के इस्लाम विरोधी गए और उनसे यह कहा कि आप अगर अपने इस भतीजे को इस नए दीन के आमंत्रण से रोक दें तो जो कुछ यह कहेंगे हम वह सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और दूसरे भी बहुत-से प्रस्ताव रखे जिनसे आप लोग वाक़िफ़ हैं। जवाब में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “मैं उनसे केवल यह चाहता हूँ कि यह एक कलिमे को मान लें तो अरब के लोग उनके सामने सिर झुका लेंगे और अजम उनके सामने झुक जाएँगे।” गोया इस्लाम के कलिमा-ए-तय्यिबा के बीज में ये फल पहले दिन से मौजूद थे और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने समय-समय पर उसका इज़हार भी किया।
सम्भवत: दूसरी बैअते-उक़बा के मौक़े पर जब मदीना मुनव्वरा के प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से यह बात तय हो गई कि अब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आपके सहाबा हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना चले जाएँगे, तो एक सहाबी ने अंसारियों से पूछा कि “तुम्हें मालूम है कि किस चीज़ पर बैअत कर रहे हो? इस बैअत के परिणामस्वरूप पूरे अरब और अजम से तुम्हारा मतभेद हो जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?” उन्होंने कहा कि “हाँ हम तैयार हैं!” गोया बैअत करनेवालों को मालूम था कि किस काम के लिए बैअत कर रहे हैं और बैअत लेनेवालों को भी पहले दिन से यह मालूम था कि किस काम की बैअत हो रही है। यह ऐसी चीज़ नहीं थी कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने, अल्लाह की पनाह! मदीना की परिस्थितियों को देखकर इरादा बदल दिया और सत्ता के रास्ते पर चल पड़े। यह इस्लाम और उम्मत की रक्षा के लिए ज़रूरी था और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुस्लिम समाज को जिस चरित्र के लिए तैयार करना था उस चरित्र को निभाने के लिए यह सारी शक्ति और संसाधन अपरिहार्य थे। ग़ज़वा-ए-ख़ंदक़ का ज़िक्र आपने सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक चट्टान पर कुल्हाड़ी मारी तो फ़रमाया कि इसमें से मुझे क़ैसरो-किसरा के महल नज़र आए हैं। इस तरह के इशारे आप समय-समय पर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से करते रहते थे। जिसका उद्देश्य यह था कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) मानसिक रूप से तैयार रहें कि उनको क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी हैं और आगे चलकर क्या-क्या करना है।
इससे भी बढ़कर मदीना मुनव्वरा के आरम्भिक दौर की बात है कि एक जंग में हज़रत सफ़ाना-बिंते-हातिमताई जब क़ैद होकर आईं तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह सुनकर कि वे अरब के प्रसिद्ध सख़ी सरदार हातिमताई की बेटी हैं तो आपने उनको तुरन्त रिहा कर दिया। जब वे मुसलमानों की क़ैद से बाइज़्ज़त तौर पर रहा होकर सुरक्षित अपने घर चली गईं तो अदी-बिन-हातिम शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में हाज़िर हुए। ज़ाहिर है कि वह एक अत्यन्त सख़ी बाप के बेटे थे, एक बड़े दयालु बाप के बेटे थे जो अपनी सख़ावत (दानशीलता), शराफ़त और सदाचार में मिसाल है। उसके बेटे भी वैसे ही होंगे, शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास हाज़िर हुए। इस मौक़े पर बहुत-सी बातें हुईं। आपने इस मौक़े पर फ़रमाया कि “ऐ अदी, बहुत जल्द वह ज़माना आनेवाला है कि एक नौजवान महिला अकेली हज़्रमौत (यमन) से निकलेगी, उसके हाथ में सोना होगा। वह अकेली बालबक (लेब्नान) तक चली जाएगी, हज़्रमौत और बालबक के दरमियान जैसे लम्बे-लम्बे फ़ासलों का अकेली सफ़र करेगी। और कोई उसको तंग करनेवाला नहीं होगा।” गोया एक ऐसे राज्य की स्थापना जिसमें सुख-शान्ति का यह हाल हो और आम जनता को इतनी सुरक्षा प्राप्त हो, वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने था, आप उसकी कई बार भविष्यवाणी कर चुके थे और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए यह कहना कि यह कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बाद में सोची और लोगों पर थोप दी, यह बिलकुल ग़लत और दिग्भ्रमित करनेवाली बात है।
शब्दावलियों की समस्या
इस्लामी राज्य पर बात करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या शब्दावलियों की है। कभी-कभी कुछ विशेष शब्दावलियों पर ज़ोर देने या कुछ ख़ास शब्दावलियों को दूसरे माहौल और पृष्ठभूमि में प्रयुक्त करने से ग़लत-फ़हमियाँ और उलझनें पैदा होती हैं। यह उलझन इस्लाम के राजनैतिक और संवैधानिक मामलों पर चर्चा करते हुए ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है।
राजनैतिक व्यवस्था, संवैधानिक प्रबन्धों और राज्य सम्बन्धी मामलों के बारे में इस्लामी साहित्य में बहुत-सी शब्दावलियों प्रयुक्त हुई हैं। उनमें से कुछ शब्दावलियाँ पवित्र क़ुरआन में आई हैं, कुछ शब्दावलियाँ बाद में मुसलमानों ने अपनाईं। जबकि कुछ शब्दावलियाँ हमारे इस दौर में भी अपनाई गईं। कुछ शब्दावलियाँ तो वे हैं जो पवित्र क़ुरआन ने निश्चित रूप से कुछ अर्थ समझाने के लिए प्रयुक्त की हैं और मुसलमान उन अर्थों को बयान करने के लिए आम तौर पर उन्हीं शब्दावलियों को प्रयुक्त करते हैं। इस तरह उदाहरणार्थ ज़कात, हज, जिहाद की शब्दावलियाँ हैं। लेकिन इन शब्दावलियों का प्रयोग मुसलमानों में कभी भी फ़र्ज़ या अनिवार्य नहीं समझा गया। स्वयं पवित्र क़ुरआन ने इन शब्दावलियों के प्रयोग को अनिवार्य क़रार नहीं दिया है। उदाहरणार्थ पवित्र क़ुरआन में कहीं यह माँग नहीं की गई है कि जंग के लिए जिहाद ही का शब्द प्रयुक्त करो। स्वयं पवित्र क़ुरआन में जंग के लिए जिहाद के साथ-साथ क़िताल की शब्दावली भी प्रयुक्त हुई है। इसी तरह से इस्लामी साहित्य में जंग और हर्ब की शब्दावलियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। स्वयं हमारे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और तुर्की आदि में सलात की बजाय नमाज़ की शब्दावली प्रयुक्त होती है। हालाँकि ये वे शब्दावलियाँ हैं जो ख़ास इस्लामी अर्थों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। उनका प्रयोग भी किसी फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा नहीं रखता। अगरचे बेहतर और उत्तम है।
इसके विपरीत कुछ और शब्दावलियाँ हैं जो पवित्र क़ुरआन ने मात्र किसी ख़ास अर्थ को ज़ेहन में बिठाने के लिए प्रयुक्त की हैं। उनको प्रयुक्त करना या उनको अपनाना भी किसी तरह अनिवार्य और आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन ने बादशाह की शब्दावली भी प्रयुक्त की है। सूरा बक़रा में है कि एक पैग़ंबर से लोगों ने गुज़ारिश की कि दुआ करें कि सर्वोच्च अल्लाह हमारे लिए एक बादशाह निर्धारित कर दे। (आयत-246) पैग़ंबर ने अल्लाह के आदेश से उनको बताया कि सर्वोच्च अल्लाह ने तालूत को तुमपर बादशाह बनाकर भेजा है। (आयत-247) गोया मुसलमानों के प्रमुख को बादशाह भी कहा जा सकता है। इसी तरह से पवित्र क़ुरआन में एक जगह बनी-इसराईल को सम्बोधित करके कहा गया है कि अल्लाह की इस नेअमत को याद करो जब अल्लाह ने तुममें नबी भेजे और तुम्हें बादशाह बनाया। गोया बादशाह बनाना सर्वोच्च अल्लाह की एक नेमत है। लेकिन बादशाह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे बादशाहों से बचना चाहिए और अच्छे बादशाहों की पैरवी करनी चाहिए। कुछ आयतों में ख़िलाफ़त का शब्द भी आया है। इसलिए आरम्भिक सदियों में कुछ मुस्लिम शासक ख़लीफ़ा कहलाए कुछ नहीं भी कहिलाए। सुल्तान का शब्द भी पवित्र क़ुरआन में आया है इसलिए कुछ मुसलमान शासक सुल्तान भी कहलाए। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पवित्र क़ुरआन ने किसी ख़ास शब्दावली के प्रयोग की अनिवार्य शिक्षा नहीं दी। अगरचे मुसलमानों के लिए उचित और बेहतर यही है कि वही शब्दावलियाँ प्रयुक्त करें जो पवित्र क़ुरआन में आई हैं और जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने प्रयुक्त की हैं।
अस्ल चीज़ यह है कि किसी संस्था का उद्देश्य और मूलात्मा क्या है। जो उद्देश्य है वह इन चार चीज़ों में बयान हो चुका। ये चार चीज़ें वे हैं कि अगर कोई राज्य उनको अंजाम दे रहा है और राज्य शरीअत के आदेशों के अनुसार काम कर रहा है तो वह राज्य पूर्ण रूप से इस्लामी राज्य है। इस राज्य के प्रमुख का जो भी नाम हो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन अगर राज्य के प्रमुख का नाम ख़लीफ़ा और अमीरुल-मोमिनीन हो, और वह शरीअत के एक-एक आदेश को तोड़ रहा हो और पवित्र क़ुरआन के एक-एक आदेश का उल्लंघन कर रहा हो तो फिर मात्र ख़लीफ़ा कहलाने से वह राज्य इस्लामी राज्य नहीं बन जाएगा। मात्र शासक के ख़लीफ़ा या अमीरुल-मोमिनीन कहलाने से कोई राज्य इस्लामी राज्य नहीं कहला सकता, लेकिन अगर इस्लाम के आदेशों के अनुसार राज्य की व्यवस्था चल रही है, अदालतें शरीअत के अनुसार फ़ैसले कर रही हैं और सूरा-22 (हज) की आयत-41 में बयान किए गए ये चारों उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तो चाहे राज्य में कुछ और शब्दावलियाँ प्रयुक्त हो रही हों, लेकिन पवित्र क़ुरआन की दृष्टि से उस राज्य को ग़ैर-इस्लामी नहीं, बल्कि इस्लामी राज्य ही कहा जाएगा।
मुस्लिम राज्यों में ऐसे-ऐसे शासक गुज़रे हैं कि जो तक़्वा (ईशपरायणता) और ईमान की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पर थे। नैतिक आचरण और ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त उच्च स्तर पर थे। अब्दुल-मलिक-बिन-मरवान जो बनी-उमैया के बड़े प्रसिद्ध शासक गुज़रे हैं, वे ज्ञान और तक़्वा के इतने उच्च स्तर पर थे कि हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उनके देहान्त के समय लोगों ने पूछा कि अगर आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएँ तो हम दीनी मार्गदर्शन और फ़िक़ही मामलात में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करें? हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि “मरवान के बेटे अब्दुल-मलिक से”। इमाम मालिक (रह॰) ने मुवत्ता में कई जगह यह बयान किया है कि मेरे नज़दीक अमुक काम सुन्नत है क्योंकि मैंने अब्दुल-मलिक-बिन-मरवान को यह काम करते हुए देखा है। इससे अनुमान होता है कि इमाम मालिक (रह॰) अब्दुल-मलिक के तर्ज़े-अमल को सुन्नत समझते थे। यही अस्ल चीज़ है कि राज्य में शरीअत के आदेशों के अनुसार सारा काम हो रहा हो। अब्दुल-मलिक के ज़माने में ऐसा ही हो रहा था। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने के नियुक्त किए हुए क़ाज़ी शुरैह और दूसरे क़ाज़ी मौजूद थे। वे इसी तरह से काम कर रहे थे। शरीअत के अनुसार राज्य के तमाम मामलात चल रहे थे। शासक उस सतह का था जिसका उदाहरण आप सुन चुके हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इस्लामी इतिहास में बुरे और कमज़ोर चरित्र के शासक भी हुए। लेकिन अगर इस कमज़ोर चरित्रवाले शासक के दौर में भी शरीअत के आदेशों पर अमल हो रहा हो और ये चार उद्देश्य किसी-न-किसी तौर पूरे हो रहे हों तो भी इस कमज़ोरी के बावजूद उस राज्य को इस्लामी राज्य कहा जाएगा।
सारांश यह कि राज्य का उद्देश्य और मूलात्मा यह है कि सबसे पहले तो अल्लाह के प्रभुत्व पर कार्यान्वयन हो रहा हो। दूसरी बात यह कि उस राज्य में शरीअत के आदेशों का वर्चस्व हो। शरीअत उस देश में श्रेष्ठ क़ानून हो। शरीअत से टकराती कोई चीज़ स्वीकार्य न हो और हर चीज़ के अच्छे और बुरे होने का आख़िरी और फ़ाइनल स्तर केवल शरीअते-इलाही हो। अगर कोई चीज़ शरीअत के तराज़ू पर पूरी उतरती हो तो वह स्वीकार्य हो और अगर शरीअत के तराज़ू पर पूरी न उतरती हो तो वह स्वीकार्य न हो। तीसरी और आख़िरी चीज़ यह है कि जमहूर यानी जनसाधारण को यह अधिकार हो कि जिसपर वह विश्वास रखते हों और जिसको पसन्द करते हों वही उनका शासक हो, इसी तरह उनको यह अधिकार भी हो कि अगर किसी शासक को नापसन्द करते हों तो उससे जान छुड़ा लें। यह आख़िरी शिक्षा है जिसका कभी-कभी इस्लामी इतिहास में उल्लंघन किया गया। और कई लोगों ने किया। उल्लंघन करनेवालों के साथ सर्वोच्च अल्लाह क्या सुलूक करेगा, हम नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों ने उल्लंघन किया तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि उल्लंघन किया। लेकिन शेष दो पहलुओं पर इस्लाम के इतिहास के अधिकतर दौर में अमल होता रहा है। सर्वोच्च अल्लाह की हाकिमियत को भी राज्यों ने स्वीकार किया और शरीअत के आदेशों के वर्चस्व पर भी बड़ी हद तक कार्यान्वयन होता रहा और इसको लोग मानते रहे।
लोकतंत्र का शासनाधिकार
लोकतंत्र का शासनाधिकार पवित्र क़ुरआन की आयतों और हदीसों दोनों से साबित है। पवित्र क़ुरआन में है कि “अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो और उन अधिकारियों की भी पैरवी करो जो तुममें से हों।” (क़ुरआन, 4:59) अरबी टेक्स्ट में वर्णित शब्द ‘मिनकुम’ की व्याख्या करते हुए क़ुरआन के टीकाकार और फ़ुक़हा ने लिखा है कि ‘मिनकुम’ से अभिप्रेत वे लोग हैं जिनपर जनसाधारण को भरोसा हो और वे आम लोगों में से हों। वे लोग मुसलमानों में से हों। एक हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि तुम्हारे बेहतरीन शासक वे हैं जिनसे तुम प्रेम करते हो और वे तुमसे प्रेम करते हों। तुम उनके लिए दुआ करते हो और वे तुम्हारे लिए दुआ करते हों। और तुम्हारे बदतरीन शासक वे हैं जो तुमसे नफ़रत करते हों और तुम उनसे नफ़रत करते हो। वे तुमपर लानत भेजते हों और तुम उनपर लानत भेजते हो। एक जगह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि जब तक तुम्हारे अधिकारी यानी तुम्हारे नेता तुम्हारे बेहतरीन लोग हों, जब तक तुम्हारे दौलतमंद तुममें सबसे सख़ी (दानशील) लोग हों और जब तक तुम्हारे मामलात तुम्हारी आपसी सलाह से तय हो रहे हों उस समय तक ज़मीन की पीठ तुम्हारे लिए ज़मीन के पेट से बेहतर है। और जब तुम्हारे अधिकारीगण तुममें से बदतरीन लोग हों और जब तुम्हारे दौलतमंद तुममें सबसे कंजूस लोग हों और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में आ गए हों तो ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए ज़मीन की पीठ से बेहतर है। ये तीन चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आदर्श के तौर पर बताईं। एक आदर्शवादी और स्तरीय इस्लामी समाज का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उस समाज में नेतृत्व बेहतरीन लोगों के हाथ में है या बदतरीन लोगों के हाथ में। इस ज़माने के हिसाब से जो भी बदतरीन और बेहतरीन का पैमाना है। ज़ाहिर है आज बेहतरीन का पैमाना वह नहीं होगा जो ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में था। इस पैमाने के अनुसार तो आज के बेहतरीन भी शायद उस दौर के बदतरीन से कमतर ही हों। जिस दौर में बात हो रही है उस दौर की दृष्टि से बेहतरीन लोग शासक होने चाहिएँ। अगर बदतरीन लोग नेतृत्व और सत्ता के पद पर आसीन हैं तो आदर्श समाज की पहली शर्त समाप्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि यह देखो कि इस समाज और इस दौर के दौलतमंद लोग सबसे सख़ी हैं या सबसे कंजूस हैं। यह भी देखने की बात है हमारे सामने हमारे आसपास में। और आख़िरी बात देखने की यह है कि क्या मामलात मुसलमानों के सामूहिक मश्वरे से तय हो रहे हैं या मुहल्लों की कुछ प्रभावशाली औरतों के हाथ में हैं। इससे यह न समझिएगा कि यहाँ शरीअत ने औरतों को सामूहिक मामलों से निकाल दिया है। बिलकुल नहीं निकाला। स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) महिलाओं के साथ मश्वरा किया करते थे। आम मामलात में वोटिंग की दृष्टि से वे मश्वरा देने की पाबन्द हैं और उनको मश्वरा देने में आगे-आगे होना चाहिए। यहाँ “मामले औरतों के सिपुर्द हैं” का अर्थ यह है कि जो औरतें शासकों के क़रीब हों, उनके मश्वरे और कानाफूसी से और उनकी पसन्द एवं नापसन्द के आधार पर मामलात तय पाने लगें। जब किसी क़ौम का पतन का समय होता है तो ऐसा ही होने लगता है। आप विभिन्न समयों के पतन के इतिहास पढ़ें। मुग़लों, तुर्कों और उस्मानियों के पतन के समय का इतिहास पढ़ें तो विभिन्न दरबारों और विभिन्न शासकों के घरों और आसपास में ऐसी चरित्रहीन औरतें हावी थीं या चरित्रहीन नहीं भी थीं तो ऐसी कम समझ औरतें हावी थीं जो मामलों में हस्तक्षेप कर गई थीं और अपने सीमित हितों की ख़ातिर शासकों को ग़लत रास्तों पर चलाया करती थीं। बड़े-बड़े संकट उन औरतों की तरफ़ से पैदा हुए। उदाहरण अगर दूँ तो इस समय दर्जनों उदाहरण ज़ेहन में आ रहे हैं, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ।
शाहजहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के अत्यन्त सफल, दीनदार, नेक और निष्ठावान बादशाहों में से हैं। उनके दौर में पूरे मुग़ल भारत में सुख-शान्ति का दौर-दौरा था। उनका एक अत्यंत ईमानदार और निष्ठावान मुसलमान प्रधानमंत्री नवाब सादुल्लाह ख़ान था, जो अत्यन्त दीनदार, माहिर और योग्य प्रबन्धक था और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी का सहपाठी था। इससे अनुमान कर लें कि जब मुजद्दिद साहब का क्लास फ़ेलो वज़ीरे-आज़म होगा तो हुकूमत पर दीनी प्रभाव कैसे होंगे। शाहजहाँ की एक चहेती पत्नी ने उसके ज़ेहन में यह डाला कि उत्तराधिकार मेरे अमुक बेटे को मिलना चाहिए। उत्तराधिकार का मामला किसी एक माँ या दूसरी माँ की सन्तान होने के आधार पर तो तय नहीं होना चाहिए था। योग्यता और प्रतिभा इस आधार पर होना चाहिए था कि जनसाधारण किसको पसन्द करते हैं और किसपर भरोसा करते हैं। उसका अनुभव कैसा है। इस्लाम से लगाव किसका गहरा है। शाहजहाँ ने अपनी सारी नेकी और तक़्वा के बावजूद अपनी पसंदीदा पत्नी के कहने पर ये सारी चीज़ें भुला दीं और यह चाहा कि शेष तमाम उम्मीदवारों को, जिनमें औरंगज़ेब आलमगीर भी शामिल था, वंचित कर दें और एक ऐसे शहज़ादे को जिसकी गुमराही पर इस ज़माने के दीनदारों में से अधिकांश का मतैक्य था। जिसकी नास्तिकता, भौतिकता और दीन से दूरी प्रसिद्ध एवं जानी-मानी थी, हुकूमत की बागडोर सौंप दें। दाराशिकोह जिसको शाहजहाँ ने उत्तराधिकार के लिए आगे लाना शुरू किया नास्तिकता प्रिय था। उस दौर की तमाम ग़ैर-इस्लामी और नकारात्मक शक्तियाँ उसके पीछे थीं। दारा की गुमराही के बारे में अल्लामा इक़बाल का शेर आपने सुना होगा जिसका अनुवाद कुछ यों है, “वह नास्तिकता जिसका बीज अकबर ने बोया था वह दोबारा दाराशिकोह की प्रकृति में परवान चढ़ गया था।” यानी शाहजहाँ ने दाराशिकोह को उत्तराधिकारी बनाया तो गोया कुछ औरतों के कहने-सुनने से महत्वपूर्ण मामलात को तय करने के ये परिणाम हैं। सब लोगों के मश्वरों के विपरीत केवल सीमित और अपनी चहेती औरतों की कानाफूसी के आधार पर फ़ैसले करने के दुष्परिणाम पूरे मुस्लिम भारत को देखने पड़े। ये साज़िशें, चक्करबाज़ियाँ और आपस के ख़ानदानी सम्बन्ध, और सौतनों के मतभेदों में पूरी क़ौम और हुकूमत का नुक़्सान कराना। औरतों की आपस की दुश्मनी की कोई भी वजह हो, लेकिन इसके नुक़्सानात पूरी क़ौम को उठाने पड़ते हैं। इससे यह न समझिएगा कि इस तरह मैं औरतों को बुरा कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह की स्थिति का उल्लेख है कि जब यह होने लगे तो ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए उसकी पीठ से बेहतर होगा।
जनसाधारण की पसन्द कैसे मालूम की जाएगी। इसका कोई ख़ास तरीक़ा पवित्र क़ुरआन ने नहीं बताया है। पवित्र क़ुरआन ने एक बड़ी तत्वदर्शिता के तहत यह तरीक़ा नहीं बताया। इसलिए कि यह चीज़ अनुभवों और परिस्थितियों के बदलने से बदलती रहती है। एक आदिवासी समाज में इसका तरीक़ा और होगा। एक छोटे नागरिक राज्य में इसका तरीक़ा और होगा और एक बड़े साम्राज्य में इसका तरीक़ा और होगा। एक नागरिक प्रकार की हुकूमत में और होगा और देहाती अंदाज़ की हुकूमत में और होगा। इसलिए कि किसी एक निर्धारित कार्य पद्धति को अनिवार्य क़रार देने का मतलब यह है कि जहाँ वह परिस्थितियाँ न हों वहाँ वह कार्य पद्धति नहीं चल सकेगी। यह चीज़ पवित्र क़ुरआन के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। क़ुरआन केवल मौलिक सिद्धान्त बयान करता है। केवल आम मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। व्यावहारिक विवरण जो परिस्थितियों और ज़माने के हिसाब से बदल सकते हों उन विवरणों को पवित्र क़ुरआन बयान नहीं करता।
इसलिए पवित्र क़ुरआन ने यह विवरण छोड़ दिया है। अब आदेश केवल यह है कि शासक वह हो जिसको जनसाधारण पसन्द करते हों और इसको जनता का भरोसा प्राप्त हो। वे लोग शासक न हों जिनको जनसाधारण पसन्द न करते हों। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन प्रकार के लोगों पर लानत की। उन फटकारे लोगों में ऐसा लीडर और नेता भी शामिल है जो अपनी क़ौम के सिर पर ज़बरदस्ती सवार हो जाए। उनकी मर्ज़ी के बिना उनके मामलात अपने हाथ में ले-ले।
ये और इस विषय की अनेक हदीसों से यह उसूल तो स्पष्ट तौर पर सामने आ जाता है कि शासक और नेता वे लोग हों जो उम्मत में बेहतरीन हों और जिनपर उम्मत के लोगों को भरोसा हो। लेकिन शरीअत ने इस भरोसे की प्राप्ति का कोई निर्धारित और लगा-बंधा तरीक़ा नहीं बताया। इसकी वजह केवल यह है कि यह निर्धारण केवल परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि सिरे से किसी तरीक़े की आवश्यकता ही पेश नहीं आती। अगर कभी क़ौम के नेता और विश्वसनीय लोग स्वयं ही नुमायाँ हो जाएँ और जनसाधारण और लोगों को उनपर पूरा भरोसा क़ायम हो जाए तो किसी विधिवत औपचारिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं रहती। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सरदार या नेता हों जिनपर लोग भरोसा करते हों। ये नेता जिसपर मतैक्य करें लोग उसको मान लें। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों में फ़र्ज़ कीजिए कि यह निर्धारण करना अभीष्ट हो कि पाकिस्तान का नेता कौन हो। अब यहाँ आप ग़ौर करें तो देश में पंद्रह-बीस के लगभग ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति पाते हैं कि अगर वे किसी एक आदमी पर मतैक्य कर लें तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 99 प्रतिशत लोगों ने मान लिया। ऐसे बड़े-बड़े प्रभावशाली नेता और सरदार अगर मिलकर कहें कि हम अमुक व्यक्तित्व को पाकिस्तान का नेता मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के 99 प्रतिशत लोगों ने मान लिया। मुश्किल से एक प्रतिशत रह जाएँगे जो इस राय से सहमत न होंगे। ये लोग नज़रअंदाज़ किए जा सकते हैं। इसलिए अगर कल यह कहा जाए कि ऐसे बड़े-बड़े पच्चीस-तीस आदमी मिलकर पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए जिस उचित व्यक्ति का निर्धारण कर दें तो ऐसा करना बिलकुल इस्लाम के अनुसार होगा, इसलिए कि इससे वह उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा जो दूसरे माध्यमों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं यह पच्चीस व्यक्ति नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और चारों राज्य सभाएँ मिलकर तय करें, तो शरई रूप से वह भी ठीक है। इस तरह भी जो चुनाव होगा वह ठीक शरई चुनाव होगा। लेकिन अगर आप कहें कि यह तरीक़ा भी आपके नज़दीक उपयुक्त नहीं, बल्कि adult frunchise और वयस्क मतदान के तहत हर वयस्क नागरिक वोट दे, तो यह तरीक़ा भी शरई रूप से सही है। इस तरह अगर आप अमेरिकी व्यवस्था के अनुसार पहले इलेक्टर्स का चुनाव करेंगे तो यह भी सही है। बहरहाल ये तरीक़े समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। उनमें से कोई भी तरीक़ा इस्लामी संविधान और व्यवस्था में अपनाया जा सकता है, बशर्तिके उसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों की निशानदेही हो जाए जिनपर अधिक लोगों को भरोसा हो। अगर किसी समय किसी देश में कोई एक व्यक्तित्व ऐसा मौजूद हो जिसपर जनसाधारण को इतना भरोसा हो कि मात्र उसके नामांकित कर देने से लोग किसी व्यक्ति को प्रमुख मान लें तो ऐसे व्यक्ति की तरफ़ से नामांकन भी काफ़ी है। उदाहरणार्थ हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपने बाद अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया था और आम लोगों ने मान लिया। कुछ लोग हज़रत हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस फ़ैसले पर आपत्ति करते हैं कि उन्होंने अपने देहान्त से पहले एक ख़त क्यों लिखवाया और उसमें हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को क्यों नामित कर दिया और यह क्यों कहा कि मैंने अपने बाद तुम्हारे लिए उमर-बिन-अलख़त्ताब को नामित कर दिया है, अत: इनकी बैअत कर लो। लेकिन अगर यह मौलिक सिद्धान्त ज़ेहन में हो कि मूल उद्देश्य कोई ख़ास कार्य पद्धति या प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव और निर्धारण करना है जो उम्मत में बेहतरीन हो और मुसलमानों के अधिकांश लोग उसपर भरोसा करते हों, तो अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) का फ़ैसला बिलकुल शरीअत के अनुसार और वास्तविकता पर आधारित था।
आज से लगभग तीस वर्ष पहले दिसंबर 1974 की बात है। मैं क़ायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ा रहा था। वहाँ मैंने यही बात बयान की कि एक अत्यन्त मुहतरम और लोकप्रिय व्यक्तित्व के नियुक्त कर देने से सभी प्रमुख राज्य का चुनाव अस्तित्व में आ सकता है। जैसा कि इमाम ग़ज़ाली ने एक जगह लिखा है। वह कहते हैं “अगर कोई एक ही व्यक्ति ऐसा हो जिसका अनुसरण और पैरवी सब लोग करते हों और वह दरकार गुणों से विभूषित भी हो, वह अगर किसी की बैअत कर ले तो काफ़ी है। इसपर एक विद्यार्थी ने आपत्ति की कि यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी के कहने पर सब लोग मान लें। उस समय मैंने उनको एक उदाहरण दिया। आज मैं अपने ज़माने के दो उदाहरण दे सकता हूँ। उनसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि 11 अगस्त 1947 को क़ायदे-आज़म मुहम्मद अली जिनाह ज़ियारत से रेडियो पर भाषण देते और कहते कि मैं समझता हूँ कि मेरा आख़िरी समय है और मैं अब ज़्यादा देर तक ज़िन्दा नहीं रहूँगा। इसलिए मैं अमुक साहब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। आप उनको अपना लीडर मान लें। तो क्या पाकिस्तान में कोई एक आदमी भी ऐसा होता जो कहता कि मैं नहीं मानता और इस प्रस्ताव से मतभेद करता हूँ। कहने लगे कोई न होता। मैंने कहा कि इसी लिए कहते हैं कि अगर किसी स्थिति में कोई एक आदमी ऐसा हो जिसके भरोसे पर पूरी क़ौम को भरोसा हो जाए तो उसके कहने पर समझा जाएगा कि पूरी क़ौम को भरोसा है।
दिसंबर 74 में तो यह एक ही उदाहरण मेरे सामने था। लेकिन अब एक दूसरा उदाहरण भी हमारे ही ज़माने का मौजूद है। यह बात फ़रवरी 1979 की है। ईरान में इंक़िलाब आ चुका था। ईरान का शासक देश से फ़रार हो चुका था और जाने से पहले शाहपुर बख़्तियार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुका था। लेकिन परिस्थितियों को अत्यन्त प्रतिकूल पाकर वह भी प्रधानमंत्री हाऊस से भाग गया था। यह वह दिन था जिस दिन आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़्रांस से आकर तेहरान पहुँचे थे। एयर फ़्रांस का जहाज़ जब उनको लेकर तेहरान आया तो एयरपोर्ट और रनवे लोगों से इतने भरे हुए थे कि जहाज़ के उतरने की जगह नहीं थी। पूरा तेहरान उनके स्वागत के लिए आया था। कहा जाता है कि शायद पूरे तेहरान में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी को अपना लीडर न मानता हो। हालाँकि किसी ने उनको नियुक्त नहीं किया था। कोई वोटिंग या इलेक्शन कुछ भी नहीं हुआ था। वह जलावतनी के जीवन से जब तेहरान पहुँचे और जहाज़ से उतरे तो उस समय शायद कुछ विर्द (होंठों ही होंठों में कोई दुआ पढ़ना) या तिलावत (क़ुरआन पाठ) कर रहे थे। किसी ने उनको बताया कि शाहपुर बख़्तियार भाग गया है और देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की तुरन्त आवश्यकता है। उन्होंने काग़ज़ के एक पुर्ज़े पर लिखा ‘मह्दी बाज़रगान’। बस यही शब्द लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। इस एक चिट पर मह्दी बाज़रगान का नाम लिखने से मह्दी बाज़रगान प्रधानमंत्री हो गए और न केवल ईरान के लोगों ने मह्दी बाज़रगान को प्रधानमंत्री स्वीकार किया, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने उसको प्रधानमंत्री मान लिया। यों एक नामांकित प्रधानमंत्री ने एक अत्यन्त लोकप्रिय प्रधानमंत्री की तरह दो वर्ष तक ईरान की व्यवस्था चलाई। कहने का तात्पर्य यह कि इस तरह की स्थिति भी पेश आ सकती है। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने कार्य पद्धति के विवरण और छोटी-छोटी बातों से बहस नहीं की। इसलिए कि उद्देश्य और लक्ष्य केवल यह है कि शासक वह हो जिसको जनसाधारण का भरोसा प्राप्त हो। इस भरोसे का निर्धारण कैसे होगा इसके लिए कोई भी व्यावहारिक, उचित और प्रचलित तरीक़ा हो सकता है।
शरीअत का वर्चस्व
जमहूर या लोगों की अधिक संख्या के इस अधिकार एवं भरोसे के बाद तीसरा अति महत्वपूर्ण आधार यह है कि राज्य में शरीअत का बोलबाला हो। हुकूमत की तमाम संस्थाएँ शरीअत के अनुसार काम कर रही हों। इस्लामी हुकूमत का अस्ल और मौलिक कार्य उस शरीअत को लागू करना है जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लेकर आए हैं। इमाम मुहम्मद ने ‘सियरे-कबीर’ में लिखा है “इमाम या हुकूमत का प्रमुख उस शरीअत को लागू करने का पाबन्द है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान की।” इसलिए इस्लामी राज्य का मूल उद्देश्य इस्लामी क़ानून की रक्षा और शरीअत को लागू करना है और हुकूमत उसका ज़रिया है। दूसरी व्यवस्थाओं में राज्य मूल उद्देश्य है और क़ानून राज्य को चलाने का एक ज़रिया है। इस्लाम में क़ानून यानी शरीअत मूल उद्देश्य है। राज्य उसको लागू करने का मात्र एक ज़रिया और साधन है। इस्लाम में शरीअत पहले थी, राज्य बाद में अस्तित्व में आया। शरीअत तो मक्का मुकर्रमा से अवतरित होनी शुरू हो गई थी, राज्य मदीना मुनव्वरा में जाकर क़ायम हुआ। अत: यहाँ क़ानून पहले है और राज्य बाद में है। दूसरी व्यवस्थाओं में राज्य पहले होता है, और क़ानून बाद में अस्तित्व में आता है।
शूरा (परस्पर परामर्श)
एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसके विवरण तो मैंने बहुत-से नोट किए हैं, लेकिन चूँकि समय कम है इसलिए कुछ मौलिक बातें बयान करके बात समाप्त करना चाहूँगा, वह ‘शूरा’ का सिद्धान्त है। इस्लाम की सामूहिक व्यवस्था जब भी और जहाँ भी स्थापित होगी तो वह दमन के आधार पर नहीं, बल्कि ‘शूरा’ (परस्पर परामर्श) के आधार पर चलेगी। दमन यह है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह अपनी समझ और निजी पसन्द-नापसन्द के आधार पर फ़ैसले करे। दमनकारी व्यवस्था शरीअत के अनुसार दुरुस्त नहीं है। इस्लामी शरीअत के अनुसार जितने फ़ैसले होंगे वह ‘शूरा’ के आधार पर होंगे।
‘शूरा’ के शाब्दिक अर्थ बड़े दिलचस्प हैं और इससे ‘शूरा’ के वास्तविक अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। ‘शूरा’ का शाब्दिक अर्थ है शहद की मक्खी के छत्ते से शहद निकालना। इस प्रक्रिया को ‘शूरा’ कहते हैं। अब इसपर ग़ौर करें कि शहद की मक्खी के छत्ते से जब शहद निकाला जाता है तो उसकी क्या शक्ल होती है। उसकी शक्ल यह होती है कि हज़ारों मक्खियाँ हज़ारों फूलों पर जाकर हज़ारों प्रकार के रस चूस लेती हैं। एक फूल की ख़ुशबू एक तरह की है, दूसरे की दूसरी तरह की है। किसी एक फूल में एक प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी लाभ हैं, दूसरे फूलों में दूसरे प्रकार के लाभ हैं। किसी एक फूल में सर्वोच्च अल्लाह ने एक तरह की शिफ़ा (आरोग्य) रखी है और दूसरे में दूसरे प्रकार की शिफ़ा रखी है। ये हज़ारों मक्खियाँ यों हज़ारों प्रकार का रस चूसती हैं और फिर सब मिलकर शहद बनाती हैं। जब शहद तैयार हो जाता है तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि शहद की यह बूँद इस मक्खी की है और शहद की वह बूँद उस मक्खी की है और यह अमुक मक्खी की है। या यह अमुक फूल के रस की है और यह अमुक फूल के रस की है, बल्कि यह सब मिलकर एक ऐसा सामूहिक खाद्य पदार्थ बन जाता है जिसमें सर्वोच्च अल्लाह ने शिफ़ा रखी है।
गोया इस शब्द के प्रयोग से जो पैग़ाम मिलता है वह यह है कि जब ‘शूरा’ की प्रक्रिया अपनाओ तो इस तरह के उपाय और कार्य पद्धति अपनाओ कि हर व्यक्ति के पास जो तत्वदर्शिता, बुद्धि और समझ है, एक-एक से वह समझ प्राप्त कर लो। फिर उन तमाम व्यक्तिगत समझदारियों को इस तरह से एक देशी और सामुदायिक शिफ़ा बना दो कि उसमें पूरे समुदाय के लिए मार्गदर्शन का सामान हो। इस काम को करने का क्या तरीक़ा हो। इसके विवरण हर दौर के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। लेकिन वह कार्य पद्धति बहरहाल ऐसी होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को अपनी राय देने का अधिकार हो, और व्यवस्था ऐसी बनाई गई हो कि हर व्यक्ति की राय सुनी जाए, उसपर ग़ौर किया जाए और उन सब रायों के परिणामस्वरूप एक ऐसी सामूहिक समझ को तलाश किया जाए जो मुस्लिम समाज के लिए सामूहिक शिफ़ा का ज़रिया और कारण हो। इस पूरी प्रक्रिया को भरपूर अंदाज़ में करने को अरबी भाषा में ‘शूरा’ कहते हैं। पवित्र क़ुरआन में कहा है कि “मुसलमानों के मामलात ‘शूरा’ के ज़रिये चलते हैं।” (क़ुरआन, 42:38) यानी सामूहिक समझ के आधार पर फ़ैसले होते हैं। व्यक्तिगत रायों के आधार पर बुद्धि से परे फ़ैसले नहीं होते।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ‘शूरा’ के लिए सार्वजनिक निर्देश दिए हैं। हदीसों में ‘शूरा’ का महत्व, लाभ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बहुत क़ीमती निर्देश दिए गए हैं। उन सब हदीसों का अलग-अलग उल्लेख तो इस समय मुश्किल है। लेकिन उनमें जो मार्गदर्शन दिया गया है इसका ख़ुलासा यह है कि जिन लोगों से ‘शूरा’ के लिए मश्वरा लिया जाए वे ज्ञान और समझ रखते हों, वे अल्लाह के नेक और इबादतगुज़ार बन्दे हों, उम्मत (मुस्लिम समुदाय) के प्रति निष्ठावान हों, उम्मत उनपर भरोसा रखती हो। उम्मत उनको पसन्द करती हो। उम्मत उनके लिए दुआ करती हो, वे उम्मत के लिए दुआ करते हों। जिन लोगों में ये विशेषताएँ पाई जाएँगी वे लोग मश्वरा देने के योग्य होंगे। उनको पता होगा कि जनसाधारण के लिए क्या चीज़ लाभदायक है और क्या नहीं है। इन बुनियादों पर वे जो राय देंगे और इस राय के अनुसार जो फ़ैसले होंगे वे इस्लाम और शरीअत के अनुसार होंगे। यह उन मौलिक धारणाओं का सारांश था जिनपर इस्लाम का प्रशासनकि और संवैधानिक क़ानून स्थापित है। इन धारणाओं से वह ढाँचा संकलित होता है जिनके विस्तृत विवरण इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने ज़माने में संकलित किए है। उनमें कुछ विस्तृत विवरण तो वे हैं जो इज्तिहादी प्रकार के हैं। जिनमें से कुछ आज भी सम्बन्धित relevant हैं और कुछ वे हैं जिनपर आज नए इज्तिहाद की आवश्यकता है। कुछ विवरण ऐसी चीज़ों पर मुश्तमिल हैं जो इस ज़माने के हिसाब से प्रशासनकि ‘मस्लहत’ का तक़ाज़ा थीं। अगर आज की प्रशासनकि ‘मस्लहत’ उसको स्वीकार करे तो उनपर कार्यन्वयन करना लाभकारी और उचित होगा। और अगर आज की प्रशासनकि ‘मस्लहत’ किसी और उपाय या प्रशासनकि ढाँचे की अपेक्षा करती हो तो आज की प्रशासनकि ‘मस्लहत’ के अनुसार कार्यान्वयन होगा। उदाहरण के रूप में अगर इस ज़माने में राजधानी में दो जज होते थे और आज भी इसकी आवश्यकता है तो आज भी इसी तरह करना उचित होगा। बिलकुल आरम्भिक ज़माने में फ़ौजदारी और दीवानी दोनों मुक़द्दमों को एक ही अदालत देखती थी। बाद में बनी-अब्बास के आरम्भिक दौर से ही दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें अलग-अलग कर दी गईं। यह मात्र प्रशासनकि निहितार्थ के तहत किया गया। आज भी अगर दोनों प्रकार के मुक़द्दमों के लिए दो अलग-अलग अदालतों की आवश्यकता है तो दो अलग-अलग अदालतें होंगी। ये प्रशासनकि चीज़ें हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहेंगी। लेकिन शरीअत, पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के जो मौलिक आदेश हैं वे ज्यों-के-त्यों रहेंगे और उनमें परिवर्तन नहीं आएगा।
लेकिन ये आदेश विवरण से ख़ाली हैं। इसलिए कि शरीअत यह चाहती थी कि विवरण हर ज़माने और हर इलाक़े के लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करेंगे।
सवालात
सवाल : ख़लीफ़ा का आज्ञापालन तो हर हाल में सिवाए अल्लाह की अवज्ञा के फ़र्ज़ है, तो फिर लोकतंत्र में हुकूमत या राष्ट्रपति के आदेश रद्द कैसे करें? चूँकि इस सिलसिले में कोई विधिवत सिद्धान्त या क़ानून नहीं। अगर विधिवत सिद्धान्त होगा तो इसका तरीक़ा क्या होगा?
जवाब : लोकतंत्र या जहाँ लोकतंत्र न हो, बादशाहत या ग़ैर-बादशाहत, इन सब व्यवस्थाओं में शरीअत के दृष्टिकोण से मौलिक चीज़ यह है कि जो फ़ैसला हुआ है अगर वह शरीअत के अनुसार है और आम जनता के हितों पर आधारित है तो आप उसका समर्थन करें। और अगर कोई फ़ैसला, कार्रवाई या क़ानून शरीअत के ख़िलाफ़ है और जनसाधारण के हितों से टकराता है तो आप उसका विरोध करें। इस्लाम में पार्टी के आधार पर विरोध या समर्थन की कोई कल्पना नहीं है। इस्लाम में इस रवैये की कोई गुंजाइश नहीं कि कोई चीज़ शरीअत से टकरा रही हो, शरीअत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किया जा रहा हो, कोई क़ानून क़ुरआन और सुन्नत से टकराता हुआ बनाया जा रहा हो, लेकिन आप केवल इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं कि आपकी पार्टी यह काम कर रही है। यह शरीअत में जायज़ नहीं। इसी तरह से अगर कोई काम शरीअत के अनुसार हो रहा है, कोई फ़ैसला ऐसा किया जा रहा है जो शरीअत के अनुसार है, कोई क़ानून ऐसा बनाया जा रहा है जिससे शरीअत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, लेकिन आप मात्र इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि आपकी विरोधी पार्टी वह काम कर रही है। ऐसी स्थिति में न आपके लिए विरोध करना जायज़ है, न ही आपकी पार्टी के लिए जायज़ है। यह वह मौलिक चीज़ है जो इस्लाम को पश्चिमी लोकतंत्र से अलग करती है। पश्चिमी लोकतंत्र में किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का फ़ैसला अधिकतर पार्टी की पॉलिसी के अनुसार होता है। अगर पार्टी की पॉलिसी एक चीज़ के पक्ष में है तो पार्टी उसका समर्थन करती है वरना विरोध करती है।
मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि असेंबली में वोट देनेवालों को यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने वोट किस चीज़ के बारे में दिया है। पार्टी का निर्देश आता है कि अमुक मौक़े पर हाथ उठाओ तो लोग हाथ उठा देते हैं। पार्टी की तरफ़ से निर्देश आता है कि वाक-आउट करो तो लोग वाक आउट कर देते हैं। अधिकतर परिस्थितियों में वाक-आउट करनेवालों कि यह पता ही नहीं होता कि हमने क्यों वाक-आउट किया है। यह रवैया मेरे ख़याल में शरीअत के अनुसार नहीं है। मुसलमान को हर उस चीज़ का समर्थन करना चाहिए जो शरीअत और जनसाधारण के हितों के अनुसार हो। और हर उस चीज़ का विरोध करना चाहिए जिसमें शरीअत की ना-फ़रमानी हो रही हो और जनसाधारण के हितों की ना-फ़रमानी हो रही हो। चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी पार्टी से हो।
Recent posts
-

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
22 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -

फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025 -

इल्मे-फ़िक़्ह के विभिन्न विषय (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 4)
25 February 2025