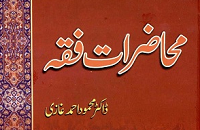
अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (लेक्चर #-9)
-
फ़िक़्ह
- at 22 March 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
आज की चर्चा की शीर्षक है ‘अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून; तत्वदर्शिता, उद्देश्य, कार्य-पद्धति, मौलिक धारणाएँ’। फ़िक़्हे-इस्लामी के इस ख़ास पहलू को चर्चा के लिए चुनने की वजह, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यह है कि आज के दौर में इस्लामी शरीअत के जिन आदेशों को बहुत ज़्यादा ग़लत समझा गया है, जिनके बारे में पूरब एवं पश्चिम में बहुत-सी नकारात्मक बातें कही जा रही हैं, ऐसी नकारात्मक बातें जिनसे मुसलमान भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, उनमें इस्लाम का अपराध और सज़ा का क़ानून भी शामिल है। फ़िक़्हे-इस्लामी का यह हिस्सा धूर्त विरोधियों और सीधे-साधे समर्थकों दोनों की ओर से नकारात्मक प्रयासों का निशाना बना हुआ है।
इस्लाम के फ़ौजदारी क़ानून के बारे में पश्चिमी लोगों के विचार
अपराध और सज़ा से सम्बन्धित इस्लामी क़ानून के बारे में जो निराधार विचार पश्चिम में फैलाए गए हैं, और जिनसे पश्चिम के एक बहुत बड़े वर्ग के अलावा पूरब में भी बहुत-से लोग प्रभावित हो रहे हैं वह यह है कि इस्लाम में सज़ाएँ बहुत पाशविक और क्रूर हैं। इस्लाम की सज़ाओं और फ़ौजदारी क़ानून के आदेशों में सामाजिक और आर्थिक तथ्यों और मानव मनोविज्ञान एवं स्वभाव का ध्यान नहीं रखा गया और प्राचीनकाल में जो पारम्परिक पाशविक सज़ाएँ प्रचलित थीं वे इस्लाम में ज्यों-की-त्यों चली आ रही हैं। ये बातें पश्चिमी जगत् में तो बहुत पहले से कही जा रही हैं। अफ़सोस है कि अब मुस्लिम जगत् में भी कुछ लोग ये बातें कहने लगे हैं। कुछ और लोग जिनका सम्बन्ध मुसलमानों ही से है, उनका यह कहने को तो जी नहीं चाहता कि उनके दीन की सज़ाएँ बर्बरतापूर्ण हैं। शायद उनकी दीन से सम्बन्धित शर्म या मुस्लिम जनाधार उनको यह बात कहने की अनुमति नहीं देता, लेकिन वे यह ज़रूर कहते हैं कि इस्लाम में जिन आयतों और हदीसों में सज़ाओं का ज़िक्र है उन आयतों या हदीसों की शाब्दिक या ज़ाहिरी व्याख्या करना उचित नहीं है, बल्कि उनमें नया इज्तिहाद करके उन आयतों और हदीसों को को नए-नए अर्थ दिए जाएँ। यह बात भी लगभग इनकार ही के समान है। इनकार खुलके किया जाए तो शायद इतना बुरा न हो जितना कि पर्दे में क्या जानेवाला इनकार ख़तरनाक होता है। देखनेवाला और सुननेवाला निष्ठावान समझे और अन्दर से इक़रार के पर्दे में इनकार और निष्ठा के रूप में त्रुटि निकालने की भावना सामने आ रही हो तो यह और भी ख़तरनाक बात होती है। कुछ और लोगों का कहना है कि जिस माहौल और समाज के लिए ये आदेश दिए गए थे, वह एक अत्यन्त उच्चस्तरीय और आदर्श परिवेश और समाज था। आजकल तो एक नापाक समाज है, कमज़ोर ईमान है, सोसाइटी अपराधों का ठिकाना बन चुकी है, इसलिए ये सज़ाएँ आज के समाज के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये बातें बहुत अधिक मुस्लिम जगत् में कही जा रही हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी ये बातें दुरुस्त स्वीकार कर ली जाएँ तो इसका अर्थ यह होगा कि सृष्टि के रचयिता, जिसने पवित्र क़ुरआन उतारा है और जिसने यह शरीअत अवतरित की है, उसको (अल्लाह की पनाह!) यह मालूम नहीं था कि आगे उसके बनाए प्राणियों (इनसानों) पर किस तरह का समय आनेवाला है और किस तरह की परिस्थितियाँ सामने आनेवाली हैं। गोया उसको न तो परिस्थितियों की ख़राबी का सिरे से अनुमान था और न ही इन परिस्थितियों की ख़राबी की शिद्दत और प्रकार का। उसने बस अपने अंदाज़े के अनुसार एक क़ानून दे दिया जो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि परिस्थितियाँ अब बहुत ख़राब हो गई हैं इसलिए इस क़ानून को तुरन्त निरस्त कर देना चाहिए और परिस्थितियों के सुधार की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
कुछ और लोग बड़े ज़ोर-शोर से यह बात कहते रहते हैं कि जब उच्च स्तरीय इस्लामी समाज अस्तित्व में आ जाएगा उस समय इन क़ानूनों के लागू करने पर ग़ौर किया जाना चाहिए। फ़िलहाल इन क़ानूनों को स्थगित रखा जाए और समाज का सारा ध्यान इस्लामी जीवन के गठन, इस्लामी उम्मत की स्थापना और इस्लामी समाज की संरचना को बहाल करने पर केन्द्रित किया जाए। जब ये सारे काम हो जाएँ उस समय सज़ाओं पर ग़ौर का नंबर आएगा।
ग़लत-फ़हमियों के कारण
ये और इस तरह की बहुत-सी ग़लत-फ़हमियाँ जो पूरब एवं पश्चिम में पाई जाती हैं, उनके तीन मौलिक कारण हैं। एक बड़ा कारण तो यह है कि दुनिया में बहुत-से लोग मानसिक रूप से पश्चिम के वर्चस्व से बुरी तरह प्रभावित हैं। उनके यहाँ हर वह चीज़ जो पश्चिम में स्वीकार्य है वह पूर्वी जगत् में न केवल स्वीकार्य है, बल्कि सच्चाई और वास्तविकता तथा न्याय और इंसाफ़ के चरम पर है। और जो चीज़ पश्चिम में अस्वीकार्य है वह यहाँ भी अस्वीकार्य है। इसलिए जब वे देखते हैं कि मुस्लिम जगत् में कुछ ऐसी धारणाएँ अभी तक मौजूद हैं जो पश्चिमी विचारों और विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं तो उनको इस्लाम का दृष्टिकोण समझने में दिक़्क़त होती है। हमारे देश में शिक्षित लोगों की एक बड़ी संख्या वह है जिनका पूरा जीवन पश्चिमी ज्ञान एवं विचारधारा को पढ़ने-पढ़ाने में गुज़रा है। पश्चिमी क़ानून, पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी आर्थिकता, पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी इतिहास, पश्चिमी साहित्य, इन सब चीज़ों के पढ़ने-पढ़ाने से उनके ज़ेहन का एक ख़ास साँचा तैयार हुआ है और वह हर मामले को उस विशेष साँचे से देखते हैं। पश्चिमी साँचा पश्चिमी विचारों एवं धारणाओं को नापने के लिए तो उपयोगी हो सकता है, परन्तु वह इस्लामी धारणाओं का जायज़ा लेने के लिए उपयोगी नहीं है। इस्लामी धारणाओं का साँचा, अच्छाई और बुराई की इस्लामी अवधारणा के आधार पर मामलों को देखता है। उसकी नज़र में बहुत-सी पश्चिमी धारणाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए एक बड़ी वजह तो इस्लाम के बारे में ग़लत-फ़हमी और इस्लाम के पक्ष को दुरुस्त तौर पर न समझने की यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बहुत-से लोग जो पश्चिमी धारणाओं से ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। और दिल में यह समझते भी हैं कि पश्चिमी धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए लेकिन उनके ज़ेहन में इस्लाम की सारगर्भिता की सही परिकल्पना नहीं है। या तो वे इस्लाम को मात्र एक धर्म समझते हैं। जैसे हिन्दू धर्म और बुद्ध मत हैं। इसी तरह वे इस्लाम को भी एक धर्म समझते हैं। या फिर वह फ़िक़्हे-इस्लामी को मात्र इस तरह की एक क़ानूनी व्यवस्था समझते हैं जिस तरह की क़ानूनी व्यवस्था एँगलो-सेक्सन लॉ है। वहाँ स्थिति यह है कि क़ानून के सीमित दायरे के बाहर एँगलो-सेक्सन लॉ को कोई दिलचस्पी नहीं कि क्या हो रहा है। समाज में कितनी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ फैल रही हैं। यह एँगलो-सेक्सन लॉ की दिलचस्पी का मैदान नहीं है। वे यह समझते हैं कि इस्लामी क़ानून भी इसी तरह का क़ानून है। कोई व्यक्ति अपने घर में क्या करता है इससे इस्लाम को भी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध रखना चाहता हूँ, इससे क़ानून और अदालत को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इस सोच से भी ग़लत-फ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं।
ग़लत-फ़हमी की तीसरी बड़ी वजह यह है कि इस्लाम की धारणाओं को ख़ास तौर पर इस्लाम के फ़ौजदारी आदेशों को उनके सही सन्दर्भ के साथ आज की भाषा में लोगों के सामने नहीं रखा गया। आंशिक रूप से लोगों ने विभिन्न बातें सुन रखी हैं कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। अमुक अपराध की सज़ा यह है और अमुक अपराध की सज़ा वह है। इन कुछ आंशिक बातों के अलावा आम तौर पर लोगों को इस्लामी क़ानून के फ़ौजदारी विभाग के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होतीं। यही वजह है कि बहुत-से शिक्षित मुसलमानों को भी एक संकलित ढंग से इस्लाम के फ़ौजदारी क़ानून को देखने और समझने का मौक़ा नहीं मिला। किसी चीज़ को आंशिक रूप से देखा और समझा जाएगा तो ग़लत-फ़हमियाँ पैदा होंगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पाँच अँधों की एक कहानी लिखी है। उन्होंने यह सुना कि उनके शहर में एक हाथी आया है। वे हाथी को देखने के लिए गए। एक अंधे ने टटोला तो उसके हाथ में हाथी का दाँत आ गया। दूसरे ने टटोला तो कान, तीसरे ने टटोला तो टांग, चौथे ने टटोला तो कमर और पाँचवें ने हाथ बढ़ाया तो सूंड हाथ लगी। जिसने टाँग को हाथ लगाया था उसने कहा कि हाथी एक स्तंभ की तरह होता है। सूंड पकड़नेवाले का ख़याल था कि हाथी साँप जैसा होता है। कमर पर हाथ फेर नेवाले का ख़याल था कि हाथी बिलकुल एक दीवार की तरह होता है। ये सारी बातें दुरुस्त भी हैं और ग़लत भी हैं। लगभग यही कैफ़ियत इस्लाम की शिक्षा के बारे में भी है। इस्लाम की शिक्षा की जानकारी न होना आम है। अच्छे ख़ासे देखनेवाले अन्धेपन का शिकार हैं। इस अन्धेपन की कैफ़ियत में इस्लाम को देखते हैं तो जो चीज़ हाथ लगती है उनके नज़दीक केवल वही इस्लाम है। और उन अधूरी जानकारियों की रौशनी में पूरे जीवन के बारे में फ़ैसले करना चाहते हैं। इससे ख़राबियाँ और ग़लत-फ़हमियाँ पैदा होती हैं।
इस्लाम एक जीनव-शैली है
इसलिए इस्लामी शरीअत के हर पहलू पर और ख़ास तौर पर फ़ौजदारी क़ानूनों पर ग़ौर करते हुए यह बात ज़ेहन में रहनी चाहिए कि इस्लाम मौलिक रूप से एक दीन (धर्म) है जो जीवन के सारे पहलुओं के लिए एक नियमावली और मार्गदर्शन है। यह एक जीवन व्यवस्था है जो जीवन गुज़ारने का एक नया ढंग बताती है। एक नया ढंग प्रदान करती है। वह ढंग और सलीक़ा जो तमाम ढंगों से भिन्न है और जीवन गुज़ारने के जितने ढंग दुनिया में प्रचलित हैं यह उनसे भिन्न है। इस्लामी जीवन व्यवस्था एक संस्कृति भी है। इसकी अपनी एक सभ्यता भी है। इस सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक क़ानून भी दरकार है। क़ानून को सफल बनाने के लिए सामाजिक जीवन के नियम भी हैं। अक़ीदे (धारणाएँ) और इबादात (पूजा पद्धति) भी हैं। इन सब चीज़ों का आपस में इस तरह का सम्बन्ध है कि ये सब चीज़ें एक-दूसरे की पूरक हैं और एक-दूसरे को बल देती हैं। नैतिक आचरण से वह माहौल पैदा होता है जिसमें लोग ख़ुद से क़ानून पर अमल करना चाहेंगे। आध्यात्मिक माहौल और इबादतों से क़ानून का पालन करने में सहायता मिलती है। शिक्षा अगर व्यापक और पूर्ण हो तो फिर इस्लाम का नैतिक आचरण, क़ानून, सामाजिक शिष्टाचार इन सबके दरमियान जो सम्पर्क है वह इंसान के ज़ेहन में स्पष्ट हो जाता है। चूँकि शिक्षा पूर्ण नहीं है और इस्लामी भी नहीं है इसलिए यह सम्पर्क स्पष्ट नहीं होता। इस्लामियात (इस्लामिक शास्त्र) की जो शिक्षा आज हमारे यहाँ दी जा रही है वह अधूरी और disjointed होती है। एक क्लास में बीस-पच्चीस किताबें छात्रों को पढ़ाई जा रही होंगी। सबसे रद्दी और संक्षिप्त किताब इस्लामियात की होगी जिसे उर्दू जाननेवाला एक बुदधिमान बच्चा एक घंटे में पढ़कर समाप्त कर सकता है। इस संक्षिप्त-सी रद्दी किताब में इस्लाम के बारे में जानकारी का वह सारा संग्रह होता है जो हम इस्लाम के बारे में अगली नस्लों को बता रहे हैं। इसमें भी हम बहुत-सी ग़ैर-ज़रूरी और सन्दर्भ से हटकर बातें बताते हैं, कि अमुक मसलक के दृष्टिकोण से अमुक चीज़ होनी चाहिए और अमुक के दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए। जगह-जगह से इसमें रिक्त स्थान (Loopholes) पाए जाते हैं। विभिन्न बुराइयों के लिए गुंजाइश निकालने का सामान भी इसमें मौजूद है। इसके परिणामस्वरूप जितना इस्लामी प्रशिक्षण होगा उसका अनुमान करना मुश्किल नहीं है। ये वे समस्याएँ हैं जिनकी मौजूदगी में इस्लाम के पक्ष को समझने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस्लामी शरीअत की आरम्भिक और परिचय सम्बन्धी चर्चा आपके सामने हो चुकी है। इस्लामी शरीअत के उद्देश्य और अद्ल एवं इंसाफ़ के बारे में भी बात हो चुकी है। यह भी सामने आ चुका कि अद्ल और इंसाफ़ शरीअत का मूल अभीष्ट है जिसके लिए पाँच चीज़ों की रक्षा ज़रूरी है और उन पाँच चीज़ों को शरीअत के उद्देश्य कहते हैं। जिनमें दीन, इंसान की जान, बुद्धि, नस्ल और माल शामिल हैं। इन पाँच उद्देश्यों और शरीअत के आम उद्देश्यों के तीन दर्जे हैं। एक दर्जा अत्यन्त अपरिहार्य आवश्यकता का है। दूसरा दर्जा आम ज़रूरत और हाजत का है। तीसरा ‘तहसीनियात’ और ‘तकमीलियात’ का है जिसकी कोई हद नहीं। शरीअत की सीमाओं के अन्दर रहते हुए जहाँ तक आप इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहे वहाँ तक आप प्राप्त कर सकते हैं।
शरीअत के उद्देश्य और इस्लाम का फ़ौजदारी क़ानून
शरीअत के पाँच मौलिक उद्देश्यों में एक मौलिक उद्देश्य इंसानी नस्ल और जान-माल की रक्षा है। इंसानी जान-माल, नस्ल और बुद्धि की रक्षा है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि इन उद्देश्यों के पूरे तौर पर नष्ट होने का ख़तरा हो तो शरीअत अत्यन्त कड़ा रुख़ अपनाती है और उन मौलिक उद्देश्यों की रक्षा के लिए सख़्त-से-सख़्त क़दम उठाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इस क़दम उठाने से पहले शरीअत ने यह कोशिश की है कि पूरे देश और समाज में एक आध्यात्मिक माहौल हो। लोगों के दरमियान अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हो। एक नैतिक वातावरण हो जिसमें हर व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता हो। सामाजिक शिष्टाचार का हर व्यक्ति पालन करता हो। आर्थिक रूप से लोग एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले हों। लोगों के मामलात इस तरह चल रहे हों कि समाज में कोई व्यक्ति मुहताज न हो। अगर मुहताज हो तो उसकी देख-भाल और भरण-पोषण करने के लिए लोग मौजूद हों। राजनैतिक दृष्टि से ऐसा प्रबन्ध हो कि जो इस्लामी अच्छाइयों को बढ़ावा दे रहा हो और बुराइयों को रोकने के कोशिश कर रहा हो। भावनात्मक दृष्टि से लोगों के स्वभाव में एक ठहराव मौजूद हो। लोगों का प्रशिक्षण हो रहा हो। लोगों का रवैया और अंदाज़ ऐसा हो कि उसमें इस्लाम के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य कार्यरत हों और आपस में एक-दूसरे के सहायक हों।
इस माहौल में अव्वल तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई अपराध घटित ही नहीं होगा। और अगर कोई अपराध घटित हो जाएगा तो समाज उसको स्वयं ही रोक देगा। अगर किसी के दिल में अपराध की इच्छा पैदा होगी तो दिल के अन्दर मौजूद ईमानी भावना उसको रोकेगी। अन्दर का ईमान नहीं रोकेगा तो सामाजिक दबाव के तहत वह अपराध नहीं करेगा। कभी-कभी इंसान अल्लाह के डर से नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव के सामने बुराई से बचता है। अगरचे यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम-से-कम इतना तो है कि इंसान बुराई से बचा रहता है। कोई आदमी शराब नहीं पीता तो शायद इसलिए न पीता हो कि लोग क्या कहेंगे कि अमुक आदमी शराब पीता है। चोरी इसलिए नहीं करता कि लोग कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ऐसा भी है और चोरी भी करता है। अगर अल्लाह के ख़ौफ़ से बाज़ नहीं आता तो कम-से-कम समाज के डर से तो बुराई से बचता है। अगर समाज में यह कैफ़ियत मौजूद हो कि उसके दबाव की वजह से लोग बुराई से बचे रहते हों तो यह चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर कोई अपराध ऐसा हो जो किसी ऐसे अपराधी के हाथों अंजाम पाए कि जिसमें उसके अपने अन्दर की ईमानी भावना भी नाकाम हो जाए, ख़ानदानी प्रशिक्षण और सामाजिक दबाव भी नाकाम हो जाए, समाज में ‘मारूफ़’ (भलाई) के पक्ष में और ‘मुनकर’ (बुराई) के ख़िलाफ़ जो एक वातावरण बना हुआ हो, वह भी उसे अपराध से रोके रखने में नाकाम हो जाए, और वह प्रत्यक्ष रूप से ऐसा अपराध कर गुज़रे जो शरीअत के किसी उद्देश्य को ध्वस्त करने के समान हो तो फिर शरीअत अपने मौलिक उद्देश्यों के बारे में कोई समझौता नहीं करती। जो व्यवस्था अपने मौलिक उद्देश्यों के बारे में समझौते करती है वह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। यह सिद्धान्त सभ्य संसार में हर जगह कार्यरत है। आज की पश्चिमी दुनिया भी अपनी धारणाओं और मौलिक उद्देश्यों के बारे में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। छोटी-से-छोटी चीज़ यहाँ तक कि अगर कोई बच्ची अपने चेहरे पर नक़ाब डाल दे, और सिर ढककर चलना चाहे, तो चूँकि यह चीज़ अप्रत्यक्ष रूप से उनके सेक्युलरिज़्म के ख़िलाफ़ है इसलिए वे इसपर कोई समझौता नहीं करना चाहते। मुस्लिम जगत् के एक अरब बीस करोड़ मुसलमानों से झगड़ा मोल लेने को तैयार हैं। लेकिन वे यह क़दम, जो उनके ख़याल में सेक्युलरिज़्म के ख़िलाफ़ है, उठाने को तैयार नहीं। यह बात हमारे लोगों को नज़र नहीं आती कि दुनिया में तमाम सिद्धान्तवादी और ज़िम्मेदार लोग हमेशा अपने मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्य के बारे में बहुत सख़्त और परिपक्व होते हैं।
इस्लाम भी अपने मौलिक उद्देश्यों के बारे में इतना ही सख़्त और पक्का है। लेकिन इस्लाम हर चीज़ को उसके सही स्थान पर रखकर सन्तुलन पैदा करना चाहता है। जो चीज़ अत्यन्त मौलिक और अपरिहार्य है उसका दर्जा सबसे ऊँचा है। जो चीज़ अपरिहार्य तो नहीं, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक साबित होती है वह ‘मुस्तहबात’ के दायरे में आती है। ‘मुस्तहबात’ के बाद शिष्टाचार का दर्जा है। उनके महत्व और उपयोगिता के बावजूद इस्लाम इन चीज़ों को बहुत मामूली समझता है और उनको इतना महत्व नहीं देता। इनमें से कुछ की तफ़सील मैं बयान कर चुका हूँ और कुछ का विवरण आगे बयान करूँगा, लेकिन मौलिक उद्देश्य जिनपर इस्लाम की सारी व्यवस्था चल रही है, उनमें भी इंसानी जान की रक्षा सर्वप्रथम महत्व रखती है जिसके तहत एक इंसान को बचाना पूरी मानवता को बचाने के समान है। और एक इंसानी जान को नष्ट करना पूरी मानवता को नष्ट करने के समान है। इस्लाम जान के बारे में कोई नरमी नहीं बरतता। इस्लाम इंसान की मान-मर्यादा के बारे में कोई कमज़ोरी स्वीकार नहीं करता। परिवार की संस्था की रक्षा के बारे में इस्लाम कोई नरमी नहीं बरतता। हर व्यक्ति के वैध तरीक़े से प्राप्त किए हुए माल की सुरक्षा को इस्लाम राज्य की ज़िम्मेदारी क़रार देता है। अगर राज्य इन पाँच चीज़ों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसके बने रहने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए इस्लाम ने अद्ल (न्याय) के जो आदेश दिए हैं और जिनके बारे में कहा गया है कि सारी आसमानी शरीअतों का और सारे पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) और तमाम आसमानी किताबों का यही एक आधार, लक्ष्य और उद्देश्य था कि लोग वास्तविक न्याय (क़िस्त) पर कार्यरत हो जाएँ। यह ‘क़िस्त’ तब ही क़ायम हो सकता है जब इन पाँच उद्देश्यों की देखभाल की जाए।
अद्ल (न्याय) और रहमत (दयालुता) का परस्पर सम्बन्ध
कुछ लोग बदनीयती या नासमझी से यहाँ एक उलझन पैदा करते हैं। कुछ अपराधों की सख़्त सज़ाओं का ज़िक्र करते हुए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सारे संसार के लिए सर्वथा दयालु होने का उल्लेख करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तो बड़े दयालु एवं कृपालु और नर्म-दिल थे, वे तो माफ़ करनेवाले थे। इसलिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऐसी सख़्त सज़ाएँ किस तरह दे सकते थे। चूँकि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) माफ़ कर दिया करते थे इसलिए आज अमुक-अमुक अपराध करनेवालों को माफ़ कर देना चाहिए। याद रखना चाहिए कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सर्वजगत् के लिए सर्वथा दयालु होने का हवाला देकर इस्लाम और मुस्लिम समाज के अपराधियों के अपराधों को अनदेखा करने की दुहाई मात्र एक प्रकार की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग (emotional blackmailing) है। यह ऐसा ही है कि कोई अपराधी पहले तो आपके ख़िलाफ़ कोई घृणित जघन्य अपराध करे और फिर आपकी माँ या परिवार के किसी और बुज़ुर्ग या किसी ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आए जिससे आपको भावनात्मक लगाव हो, उसके नाम का दुरुपयोग करके आपकी हमदर्दी प्राप्त करना चाहे। इस्लामी शरीअत में ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में हर चीज़ में मध्यमार्ग और सन्तुलन है। बुद्धि-बुद्धि की जगह और भावना-भावना की जगह है। दयालुता और न्याय दोनों एक साथ चलते हैं। न्याय को अनदेखा करके दया नहीं हो सकती। अगर न्याय की अपेक्षा को अनदेखा करके दयालुता का रवैया अपनाया जाएगा तो वह तथाकथित दयालुता दयालुता नहीं होगी, बल्कि अत्याचार बन जाएगी। दयालुता और न्याय दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और साथ-साथ चलते हैं। जो व्यक्ति दया नहीं करता वह स्वयं भी दया का पात्र नहीं है। “जो दया नहीं करता, उसपर दया नहीं की जाएगी।” यह सर्वथा दयालुता नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ही फ़रमाया है। एक आदमी दस आदमियों को क़त्ल कर दे। मरनेवाले तो दायलुता और स्नेह के पात्र न हों और क़ातिल दयालुता का पात्र हो जाए। यह मानवता के ख़िलाफ़ बग़ावत है और स्वयं मानव विरोधी एक जघन्य अपराध है कि अपराधी और हत्यारे को बराबर और समान रूप से दया का पात्र समझा जाए। उस पीड़ित को, उसके घरवालों और बच्चों को तो ममता और दयालुता का पात्र न माना जाए और स्नेह, नरमी, क़ानूनी बारीकियों, मानवता हर चीज़ को अपराधी की सेवा और प्रतिरक्षा के लिए समर्पित कर दिया जाए। यह उलझाव और असन्तुलित रवैया पश्चिम के लोगों ही को मुबारक। अल्लाह तआला की सन्तुलित और मध्यमार्गी शरीअत इससे मुक्त है। यह असन्तुलन और अपराधी के प्रति दयाभाव इस्लाम की दया की कल्पना के विरुद्ध है। इस्लाम इस तरह की दयालुता की कोई अवधारणा नहीं रखता।
अत: न्याय और दयालुता दोनों एक चीज़ हैं। न्याय की अपेक्षा दयालुता और दयालुता की अपेक्षा न्याय है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “अपने भाई की सहायता करो चाहे वह अत्याचारी हो या पीड़ित।” सहाबा ने पूछा कि “पीड़ित की सहायता तो समझ में आती है लेकिन अत्याचारी की सहायता कैसे करें?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “उसका हाथ रोक दो और उसे ज़ुल्म मत करने दो।” यानी अत्याचारी के साथ दयालुता यह है कि उसको अत्याचार करने से रोके रखो। इसलिए यह ग़लत-फ़हमी बहुत बड़ी ग़लत-फ़हमी है कि न्याय की अपेक्षाओं को नज़रअंदाज़ करके इस तथाकथित या स्वरचित दयालुता के आधार पर इस्लामी क़ानूनी व्यवस्था और न्याय और इनसाफ़ की धारणा को अनदेखा किया जाए। अगर इसकी अनुमति दे दी जाए कि हर आदमी अपनी इच्छा से यह फ़ैसला करे कि कहाँ नरमी होनी चाहिए और कहाँ सख़्ती होनी चाहिए तो फिर याद रखिए कि दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। हर अपराधी के लिए हमदर्दी की भावनाएँ रखनेवाले उसके रिश्तेदार हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह उसका भला चाहनेवाले और शुभचिन्तक होते हैं। हर अपराधी के अपराध के कुछ लाभान्वित होनेवाले या benificiaries होते हैं। अगर उनको यह अनुमति दे दी जाए कि वे फ़ैसला करें कि उनकी निजी राय में न्याय क्या है, दयालुता क्या है और न्याय तथा दयालुता की अपेक्षा क्या है, तो दुनिया की हर व्यवस्था असफल हो जाएगी।
शरीअत में दयालुता और नरमी का एक अलग स्थान है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक पूरी सुन्नत (व्यावहारिक आदर्श) इस मामले में पेश की। निजी मामलों में दयालुता और नरमी का महत्व और है। सामूहिक मामलात में दयालुता और नरमी की हैसियत और है। विशुद्ध निजी और व्यक्तिगत मामलों में हर व्यक्ति को अधिकार है कि न्याय के अनुसार अपने जायज़ ‘हक़’ को छोड़ दे और अपराधी के साथ दयालुता और नरमी से काम ले। कोई व्यक्ति मुझे नुक़्सान पहुँचाए तो मुझे शरीअत ने पूरा ‘हक़’ दिया है कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। न केवल ‘हक़’ दिया है, बल्कि इसकी नसीहत की है कि “किन्तु जो क्षमा कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है।” (क़ुरआन, 42:40) लेकिन यह ख़ालिस निजी और व्यक्तिगत मामलों में है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शान मुबारक में किसी दुष्ट ने निजी तौर पर जब भी गुस्ताख़ी की, आपकी ज़ात को कोई तकलीफ़ पहुँचाई, निजी तौर पर कोई परेशानी पैदा की तो आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जहाँ मामला ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ (मानवाधिकार) का हो, जहाँ किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान का ‘हक़’ मारा हो। वहाँ अदालत, राज्य या हुकूमत को यह ‘हक़’ नहीं पहुँचता कि किसी के ‘हक़’ को नज़रअंदाज़ करके अपराधी को माफ़ कर दे। यह हक़ अल्लाह ने इस इंसान को दिया है जिसका ‘हक़’ मारा गया है। पवित्र क़ुरआन ने प्रत्यक्ष रूप से यह ‘हक़’ दिया है, सूरा-17 बनी-इसराईल की आयत है और यह याद रखिएगा कि यह आयत हिजरत से पहले अवतरित हुई थी, जबकि अभी राज्य स्थापित नहीं हुआ था। अभी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना मुनव्वरा में नहीं आए थे, लेकिन यह आदेश अवतरित हुए जिसमें कहा गया, “जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक क़त्ल किया गया हो हमने उसके उत्तराधिकारी को यह ‘हक़’ दिया है कि वह अपना बदला ले-ले, लेकिन वह क़त्ल में ज़्यादती न करे।” (क़ुरआन, 17:33) यहाँ सर्वोच्च अल्लाह ने मज़लूम और उसके वारिसों को ‘सुल्तान’ यानी अथॉरिटी प्रदान की है। आप कौन होते हैं उससे यह अधिकार वापस लेनेवाले। अगर सारी मानवता मिलकर क़ातिल को माफ़ करना चाहे तो भी उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च अल्लाह ने यहाँ सीग़ा जमा मुतकल्लिम (उत्तम पुरुष बहुवचन) प्रयुक्त किया है। पवित्र क़ुरआन की शैली यह है कि जहाँ सर्वोच्च अल्लाह के शाहाना अंदाज़ और मालिकाना शान को बयान करना हो तो वहाँ सीग़ा जमा (बहुवचन) प्रयुक्त किया जाता है कि हमने उसके वारिस को अधिकार दिया है। इसलिए ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ में किसी कमी और रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है। ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ में फ़ैसला करने का अधिकार स्वयं पीड़ित और नुक़सान उठानेवाले को प्राप्त है। अपना ‘हक़’ लेने या न लेने और माफ़ कर देने का वह स्वयं फ़ैसला करेगा। मृतक के वारिस (या एक वारिस) ही यह फ़ैसला करेंगे कि वह अपना ‘हक़’ वुसूल करते हैं या नहीं करते।
‘हुक़ूक़ुल्लाह’ और ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’
जहाँ तक ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ (अल्लाह के अधिकारों) का सम्बन्ध है इसमें किसी वारिस को भी माफ़ करने का अधिकार नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने अल्लाह के हुक़ूक़ को नज़रअंदाज़ करके उनको तोड़ा है तो वहाँ किसी को भी माफ़ करने का अधिकार नहीं है। न वर्तमान शासक को, न राज्य को, न किसी प्रभावित व्यक्ति को न उसके रिश्तेदारों को।
कुछ मामलों के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ का और दूसरा पहलू ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ (बन्दों के अधिकारों या मानवाधिकारों) का होता है। उदाहरणार्थ चोरी की सज़ा में ये दोनों पहलू पाए जाते हैं। इसमें बन्दे का ‘हक़’ यह है कि उसका माल नष्ट हो गया और अल्लाह का ‘हक़’ यह है कि मामला ‘हुदूद’ (सज़ाओं) का है। ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ के तहत यह एक ‘हद’ (सज़ा) है और हद के मामले सारे-के-सारे अल्लाह के हुक़ूक़ हैं। इस मामले में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अगर कोई व्यक्ति मामले के अदालत में जाने से पहले-पहले माफ़ कर दे, तो उसको अनुमति है। किसी के घर में चोरी हुई और उसने उसी समय माफ़ कर दिया, वह माफ़ कर सकता है। लेकिन जब मामला राज्य के नोटिस में आ गया, हमारी व्यवस्था के तहत एफ़आईआर दर्ज हो गई, अदालत में शिकायत दायर हो गई तो फिर माफ़ी का अधिकार किसी को नहीं रहा। मस्जिदे-नबवी में एक साहब आराम कर रहे थे। एक क़ीमती चादर सिर के नीचे संभालकर रखी थी और सो रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसने चुपके से उन साहब के सिर के नीचे से चादर निकाली और चल दिया। चादर के मालिक, जो सो रहे थे उनको कुछ देर के बाद ख़याल आया कि चादर मौजूद नहीं है। निकलकर देखा तो वह व्यक्ति लेकर जा रहा था। पकड़कर ले आए और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में हाज़िर किया। आपने पूछा कि यह चादर किस की है। उसने स्वीकार किया कि इन साहब की है और मैंने चुराई है। अब शिकायत करनेवाले साहब बहुत घबराए और पूछा कि या अल्लाह के रसूल क्या मेरी चादर की वजह से मेरे भाई का हाथ कट जाएगा? मैं माफ़ करता हूँ और यह चादर उसको हदिया (भेंट) कर देता हूँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “मेरे पास आने से पहले क्यों माफ़ नहीं किया?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसपर नाराज़ी का इज़हार किया और सज़ा लागू कर दी। इससे यह उसूल निकला कि वे ‘हुदूद’ जिनमें ‘हुक़ूक़ुल्लाह’ का पहलू पाया जाता हो उनमें अगर प्रभावित व्यक्ति अदालत और राज्य के नोटिस में लाने से पहले-पहले अपराधी को माफ़ कर दे तो कर सकता है, लेकिन जब मामला राज्यकीय संस्थाओं के नोटिस में आ जाए उसके बाद किसी को भी माफ़ करने का अधिकार नहीं। अत: माफ़ी के तीन दर्जे हैं। ख़ालिस निजी मामलों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमेशा माफ़ी से काम लिया। पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह मुसलमानों को माफ़ी की नसीहत की। विशुद्ध ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ में आख़िर समय तक माफ़ करने का अधिकार रहता है। अदालती फ़ैसले के बाद भी माफ़ी का अधिकार रहता है। जहाँ ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ का पहलू प्रभावी है वहाँ अदालत के फ़ैसले के बाद भी माफ़ी हो सकती है। लेकिन जहाँ अल्लाह का हक़ और बन्दे का हक़ दोनों पाए जाते हों, लेकिन अल्लाह के हक़ का पहलू प्रभावी हो वहाँ किसी मरहले पर भी अपराधी को माफ़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं। जहाँ दोनों हुक़ूक़ (अधिकार) मिलते हों वहाँ ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ को अदालत के नोटिस में आने से पहले पहले माफ़ किया जा सकता है।
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की बयान की हुई एक प्रसिद्ध रिवायत है जिससे ये तीनों दर्जे स्पष्ट हो जाते हैं। उम्मुल-मोमिनीन कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने मुबारक हाथों से कभी भी अपने किसी सेवक को किसी नौकर या नौकरानी को, और यहाँ तक कि सवारी पर सवार होते हुए किसी जानवर तक को नहीं मारा। सवारी में लोग अक्सर चाबुक से काम लेते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जानवर पर भी चाबुक का प्रयोग नहीं किया। किसी व्यक्ति, किसी जानवर और किसी भी जानदार के ख़िलाफ़ कभी कोई चीज़ प्रयुक्त नहीं की। हाँ जब जिहाद के मैदान में होते थे, वहाँ हर तरह की क़ुव्वत और हथियार प्रयुक्त करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ख़िलाफ़ ज़्यादती की हो और आपने बदला लिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ सिवाय इस स्थिति के कि सर्वोच्च अल्लाह की नियुक्त की हुई सीमाओं को तोड़ा जाए और उनका ध्यान न रखा जाए। जब सर्वोच्च अल्लाह की हुरुमात (निषेधाज्ञाओं) को तोड़ा जाता था तो फिर कोई चीज़ आपके क्रोध एवं आक्रोश का मुक़ाबला नहीं कर सकती थी। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का क्रोध एवं आक्रोश और नाराज़ी ऐसी होती थी कि कोई उसको बर्दाश्त न कर पाता था। यहाँ तक कि अल्लाह के आदेश के अनुसार उसको सज़ा मिलती थी। स्पष्ट हुआ कि ‘हुदूदुल्लाह’ (अल्लाह द्वारा निर्धारित सज़ाओं) में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किसी प्रकार की नरमी नहीं की।
सज़ाओं को लागू करने में अपनी पसन्द की नरमी
पवित्र क़ुरआन और सुन्नत ने मात्र ये हुदूद (सज़ाएँ) बयान करने पर बस नहीं किया, बल्कि इंसानों की इस कमज़ोरी की निशानदेही भी की कि इंसान अपनी नादानी, नासमझी और कम इल्मी से व्यावहारिकता की पूरी अवधारणा को कभी-कभी नज़रअंदाज़ कर देता है और किसी सामयिक भावना या उत्प्रेरक से कोई एक पहलू उसके ध्यान का केन्द्र बन जाता है। मामलों की आम अवधारणा के उपेक्षित हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जहाँ नरमी नहीं करनी चाहिए थी वहाँ नरमी हो जाए और जहाँ सख़्ती की आवश्यकता थी वहाँ सख़्ती न हो। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह उसकी निशानदेही कर दी। यही अल्लाह की वह्य का काम है कि जहाँ मानव-बुद्धि अपने तौर पर किसी समस्या का समाधान मालूम न कर सकती हो, या किसी सवाल का जवाब खोज न सकती हो, वहाँ अल्लाह की वह्य मार्गदर्शन कर देती है। इसी तरह से अगर किसी मामले में इस बात की सम्भावना हो कि वहाँ मानव-बुद्धि ग़लती करेगी तो अल्लाह की वह्य उस ग़लती की निशानदेही करके यह बता देती है कि यहाँ यह सम्भावना मौजूद है और यह ग़लती हो सकती है। पवित्र क़ुरआन में एक जगह कहा गया है, “अल्लाह के दीन के अनुसार जब उन दोनों आरोपियों को सज़ा देने लगो तो इसमें कोई दया या नरमी तुम्हें प्रभावित न करे।” (क़ुरआन, 24:2) अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें किसी नरमी की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ने जो आदेश दिया है नरमी का तक़ाज़ा है कि उस आदेश के अनुसार अमल करो। तुम कौन होते हो यह आदेश देनेवाले कि अमुक के साथ नरमी की जाए और अमुक के साथ सख़्ती की जाए। तुम्हारा काम केवल अल्लाह के क़ानून पर स्वयं अमल करना और दूसरों से कराना है। जिसने पैदा किया है वह बेहतर जानता है और उसी को मालूम है कि क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर किसी छोटे बच्चे का ऑप्रेशन होना हो और उससे पूछा जाए कि मियाँ तुम्हारा ऑप्रेशन किया जाए कि न किया जाए, तो शायद एक लाख बच्चों में एक भी ऐसा न हो जो स्वयं यह कहे कि हाँ मेरा ऑप्रेशन कर दो। लेकिन क्या आप उस बच्चे की बुद्धि पर भरोसा करके ऑप्रेशन स्थगित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह रोए, चीख़े या चिल्लाए, आप ज़बरदस्ती पकड़कर उसका ऑप्रेशन करा देते हैं।
सच्चाई यह है कि अल्लाह के आदेश के मुक़ाबले में इंसानों की बुद्धि की इतनी भी हैसियत नहीं जितनी आपकी बुद्धि के मुक़ाबले में एक बच्चे की बुद्धि की हो सकती है। आपकी बुद्धि के मुक़ाबले में एक बच्चे की बुद्धि की जितनी हैसियत है अल्लाह के आदेश के मुक़ाबले में उतनी हैसियत भी सारे इंसानों की बुद्धि की नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने यह याद दिलाना ज़रूरी समझा कि “अल्लाह के दीन के अनुसार जब उन दोनों आरोपियों को सज़ा देने लगो तो इसमें कोई दया या नरमी तुम्हें प्रभावित न करे।” (क़ुरआन, 24:2) और “ऐ बुद्धि रखनेवालो! तुम्हारे लिए क़िसास में जीवन है।” (क़ुरआन, 2:179) यह मत समझो कि क़िसास का आदेश बहुत सख़्त है। जिसने मेरा हाथ काटा मैं उसका हाथ क्यों कटवाऊँ। जिसने एक इंसान को क़त्ल क्या हम उसको कैसे क़त्ल करवा दें। आजकल का बुद्धिजीवी वर्ग कहता है कि एक जान तो अपराध करने के परिणामस्वरूप नष्ट हो गई। दूसरी हम सज़ा देकर नष्ट कर दें। अल्लाह का आदेश है कि दूसरे इंसान को बदले में क़त्ल करो। अगर इस दूसरे को क़त्ल नहीं करोगे तो दस क़त्ल होंगे। इन दस क़त्ल की घटनाओं से बचने के लिए इस एक आदमी का क़त्ल करना ज़रूरी है। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने कहा है कि तुम्हारे लिए क़िसास में जीवन है। “ऐ बुद्धि रखनेवालो, तुम्हारे लिए क़िसास में जीवन है।” (क़ुरआन, 2:179)
अपराध के दो बड़े प्रकार
ये वे मौलिक धारणाएँ हैं जिनके अनुसार शरीअत ने अपराध और सज़ा की एक व्यवस्था दी है। इस्लामी शरीअत यह महसूस करती है कि जितने अपराध मानव समाज में पाए जाते हैं वे दो प्रकार के हैं। इंसानी अनुभव और अवलोकन इसका गवाह है। आप दुनिया में अपराधों के इतिहास का जायज़ा लें। आंकड़े जमा करें। प्राचीन जगत् और आधुनिक संसार दोनों के आंकड़े एकत्र करें तो आपको पता चलेगा कि अपराध के आम तौर से दो प्रकार होते हैं। कुछ अपराध तो वे होते हैं जो दुनिया के हर मानव समाज में पाए जाते हैं। कोई मानव समाज उन अपराधों से पूरी तरह ख़ाली नहीं होता। इसके विपरीत कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कुछ समाजों में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। उदाहरण के रूप में चोरी हर समाज में होती है। कोई समाज ऐसा नहीं जहाँ चोरियाँ न होती हों। अमेरिका और फ़्रांस में भी होती हैं, जर्मनी में भी होती हैं, भारत और पाकिस्तान में भी होती हैं। पहले भी होती थीं आज भी होती हैं। इस तरह नशा करनेवाले हर समाज में होते हैं। शराब पीनेवाले कोई और नशा करनेवाले अफ़ीम, भंग हर प्रकार का नशा करनेवाले हर देश और हर समाज में भी पाए जाते हैं। कहीं कम होते हैं कहीं ज़्यादा, लेकिन हर जगह होते हैं। नैतिक और यौन अपराध भी हर समाज में होते हैं। बड़े-बड़े सभ्य और विकसित समाजों में ये अपराध होते हैं। यहाँ तक कि बड़े-बड़े देशों के प्रमुख नैतिक और यौन प्रकार के अपराधों में लिप्त होते हैं और उनकी दास्तानें अख़बारों और रेडियो पर आए दिन बयान होती हैं। न उन तथाकथित लीडरों को शर्म आती है और न ही उनको आदर्श माननेवालों को ग्लानि महसूस होती है। इससे पता चला कि सभ्य-से-सभ्य समाजों में ये अपराध होते हैं और इससे कोई समाज मुक्त नहीं। इसलिए शरीअत ने एक प्रकार तो उन अपराधों का बताया है जो हर समाज में पाए जाते हैं। गोया इंसानों के स्वभाव को अगर सही नैतिक सीमाओं में न रखा जाए तो इसकी बहुत सम्भावना है कि वे अपराध घटित हो जाएँ। इसके विपरीत कुछ और अपराध ऐसे होते हैं जो कुछ समाजों में होते हैं और कुछ में नहीं होते। उदाहरण के रूप में खाने की चीज़ों में मिलावट का अपराध पश्चिमी दुनिया में नहीं होता लेकिन हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ दवाओं में, बल्कि खाने की हर चीज़ में मिलावट होती है। लोग कुछ पैसों की ख़ातिर लोगों की ज़िन्दगियों से खेलते हैं। पश्चिमी दुनिया में ऐसा नहीं होता। या अगर होता है तो बहुत कम होता है। कुछ अपराध उनके यहाँ होते हैं हमारे यहाँ नहीं होते।
अपराध और सज़ाएँ
शरीअत ने वे अपराध जो हर जगह होते हों उनकी बड़ी सख़्त सज़ा निर्धारित की है। और उन सख़्त सज़ाओं का उद्देश्य यह है कि मानव समाज के वे नैतिक मूल्य जो शरीअत चाहती है कि हर मानव समाज में पाए जाएँ उनकी रक्षा हो। इंसानी जान की रक्षा, इंसानी इज़्ज़त, माल और परिवार की रक्षा शरीअत के मौलिक उद्देश्यों में से है। परिवार की संस्था जब अस्तित्व में आती है तो उसका आधार दो चीज़ों पर होता है। अगर ये दो चीज़ें मौजूद न हों तो परिवार की संस्था अस्तित्व में नहीं आ सकती। और अगर इन दो के बिना अस्तित्व में आ भी जाएगा भी तो तबाह हो जाएगा। जिस तरह कि पश्चिम में तबाह हो गया है। वहाँ साठ प्रतिशत परिवार शादी के पाँच-दस वर्ष बाद टूट जाते हैं। इसलिए कि वहाँ यह मौलिक मूल्य एवं धारणाएँ मौजूद नहीं हैं।
सबसे पहली मौलिक धारणा ‘हया’ की है। उनके पास अंग्रेज़ी भाषा में ‘हया’ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ‘हया’ के लिए अंग्रेज़ी भाषा में Modesty का शब्द प्रयुक्त करते हैं जो ‘हया’ से विभिन्न चीज़ है। मोडेस्टी का अर्थ ज़्यादा-से-ज़्यादा शर्म हो सकता है, हालाँकि शर्म अलग चीज़ है, ‘हया’ अलग चीज़ है। ‘हया’ एक व्यापक शब्दावली है जिसमें ज़िम्मेदारी का एहसास, नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प, अनैतिक या अभद्र मामलों से बचने का आन्तरिक एवं स्वाभाविक उत्प्रेरक, आम चलन के ख़िलाफ़ मामलों से स्वाभाविक घृणा, ये सब चीज़ें ‘हया’ में शामिल हैं। मानव समाज का आधार अगर ‘हया’ पर हो तो अनगिनत अच्छाइयाँ ऐसी हैं जिन पर ख़ुद-ब-ख़ुद अमल होता चला जाएगा। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि हर दीन में एक मौलिक नैतिक सिद्धान्त होता है जिसको वह दीन लेकर चलता है। आप विभिन्न धर्मों को देखें। हर धर्म में किसी एक नैतिक गुण को बहुत ज़्यादा महत्व और केन्द्रीयता के साथ बयान किया जाता है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि इस्लाम में अगर किसी ऐसे नैतिक गुण को महत्व के साथ बयान किया जाए तो वह ‘हया’ है। ‘हया’ के परिणामस्वरूप हमेशा ख़ैर और भलाई ही पैदा होगी कभी बुराई पैदा नहीं होगी। यह भी एक हदीस है। यह एक मौलिक सिद्धान्त याद रखें। इस्लामी समाज और सामूहिक सम्पर्कों का आधार यह सबसे पहला उसूल ‘हया’ है।
दूसरा सिद्धान्त अद्ल और न्याय है जिसका मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। अद्ल और इंसाफ़ पूर्ण न्याय और हर सम्भव न्याय। अद्ल ज़ुल्म का विलोम है। ज़ुल्म के बारे में मैंने बताया था कि इसका मतलब है ‘किसी चीज़ को अपनी अस्ल जगह की बजाय किसी दूसरी जगह रख देना’। अगर किसी चीज़ को उसकी अस्ल जगह से हटाकर रखा जाएगा तो यह उस चीज़ के साथ ज़ुल्म है और अगर उस चीज़ को उसकी अस्ली जगह यानी उचित जगह पर रखा जाएगा तो यह अद्ल है। तलवार वहाँ प्रयोग करें जहाँ उसको प्रयोग करना चाहिए, यह अद्ल है। जहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए और आप प्रयोग करेंगे तो यह ज़ुल्म होगा। किसी को सज़ा देनी हो तो जहाँ सज़ा देनी चाहिए वहीं और उतनी ही सज़ा देना अद्ल है। और जहाँ सज़ा नहीं देनी चाहिए वहाँ सज़ा दें यह ज़ुल्म है। पैसे का उपयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ करेंगे तो अद्ल होगा और अगर नहीं करेंगे तो ज़ुल्म होगा। ज़ुल्म की इस परिभाषा को चस्पाँ करते जाएँ तो हर जगह यह शब्दावली फ़िट होती चली जाएगी।
पवित्र क़ुरआन ने ‘हुदूद’ (अल्लाह और रसूल के द्वारा निर्धारित सज़ाओं) के बारे में विशेषकर और ताज़ीरी सज़ाओं (वे सज़ाएँ जो परिस्थितियों को देखते हुए समय का शासक तय करे) के बारे में आम तौर से जो आदेश दिए हैं, उनमें शरीअत ने इस दृष्टि से अन्तर रखा है कि क्या अपराध ख़ामोशी से और ख़ुफ़िया अंदाज़ में हुआ है? या वह खुल्लम-खुल्ला हुआ है? अगर अपराध छिपकर किया गया है और उसमें बन्दे का कोई ‘हक़’ प्रभावित हुआ है तो फिर बन्दे को अधिकार है कि अदालत में जाकर अपना ‘हक़’ वुसूल करे और जो सुबूत और गवाही उसके पक्ष में पेश करना चाहता है पेश करे, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं। लेकिन अगर वह हक़ अल्लाह का ‘हक़’ है तो फिर शरीअत ने उसको दोहरा अपराध क़रार दिया है। एक तो स्वयं एक ग़लत कार्य का अपराध है। दूसरे बेशर्मी का अपराध इस ढंग से खुल्लम-खुल्ला किया गया, अपराध इस तरह किया गया कि दस-दस आदमियों ने देखा और चार गवाह उपलब्ध हो गए। यह दोहरा अपराध है। पवित्र क़ुरआन ने सूरा-24 नूर में कहा है कि ‘“जो लोग यह चाहते हैं कि मुसलमानों में अश्लीलता और निर्लज्जता फैले उनके लिए दुनिया और आख़िरत दोनों में दर्दनाक यातना है।” (आयत-19)
बुराई का अनावश्यक प्रचार
आजकल एक और ग़लत सोच भी आम हो गई है और उन संवाददाताओं ने फैलाई है जिनको इस्लामी नैतिक आचरण और ‘आदात’ की अधिक जानकारी नहीं है। वे यह कहते हैं कि समाज की बुराइयों को सामने लाना हमारा काम है। जो भी बुराई होगी हम उसको सामने लाएँगे। इस सोच के तहत वे बुराई के ऐसे-ऐसे विस्तृत विवरण छाप देते हैं जो इस्लामी समाज के स्वभाव के बिलकुल ख़िलाफ़ होते हैं। यों सबके सामने अश्लील बातों का उल्लेख और प्रचार इस्लाम के स्वभाव के ख़िलाफ़ है, बुराइयों का इस ढंग से एलान इस्लामी धारणाओं ‘हया’ और नैतिक आचरण से मेल नहीं खाता। इस्लाम का स्वभाव और शिक्षा यह है कि अगर बुराई छिपी हुई और सीमित है तो उसको छिपा हुआ और सीमित ही रखो। इसलिए कि जब बुराई फैलेगी तो इससे और लोग भी प्रभावित होंगे। बुराई का उदाहरण उस ज़हरीली गैस का-सा है जो अन्दर किसी गहरे गटर में पाई जाती है। अगर वह ज़हरीली गैस अन्दर ही बंद रहेगी तो उसका नुक़्सान कम-से-कम होगा और समय के साथ वह मिट्टी में विलीन हो जाएगी और लोग भूल जाएँगे कि यहाँ गंदगी थी और ज़हरीली गैस थी। लेकिन अगर आप दस आदमियों को किनारे पर खड़ा करके गटर का रास्ता खोल दें कि हम बुराई को छिपाना नहीं चाहते तो इससे दस आदमी इसी तरह मर सकते हैं जिस तरह रोज़ अख़बारों में आता है कि ज़हरीली गैस से इतने आदमी मर गए। इसलिए इस्लाम यह कहता है कि अगर बुराई सीमित है तो उसको सीमित ही रखो। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस व्यक्ति के बारे में नापसंदीदगी का इज़हार किया जो छिपी हुई बुराई को पब्लिक में बयान करे।
ये इस्लाम की भी विशेषता है और इंसानी स्वभाव की भी विशेषता है कि इंसान अपनी बुराइयों को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि छुपाता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि उसके अन्दर क्या गंद भरा हुआ है। मुझे भी मालूम है कि मेरे अन्दर बहुत कुछ गंद भरा हुआ है। आपको भी मालूम है। हर व्यक्ति प्रतिदिन उसको बाहर निकालता है। लेकिन क्या नैतिक आचरण, ‘हया’ और सभ्यता का तक़ाज़ा यह है कि यह गंद सबके सामने खोलकर रख दिया जाए और हर एक को दिखाया जाए कि मेरे अन्दर यह भरा हुआ था और अगर आप आपत्ति करें कि बुराई को सामने क्यों लाया गया तो मैं कहूँ कि जनाब बुराई को छिपाकर नहीं रखना चाहिए इसलिए कि हमारा काम ही यह है कि सबके सामने खुल्लम-खुल्ला यह गाते फिरें कि किसके दिलो-दिमाग और जिस्म में क्या है। सारांश यह कि इस्लामी दृष्टिकोण से यह एक अनैतिक और मात्र जाहिलाना बात है। मात्र पश्चिम की निर्लज्जता और अनैतिकता की धारणाएँ हैं जिसमें लोग बे-हयाई की बातें बयान करके दूसरों को प्रभावित करते हैं और समाज में बुराई का डर कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी दहशत कम हो जाती है। इसलिए शरीअत ने यह आदेश दिया कि बुराई को हर सम्भव प्रयास द्वारा रोका जाए और अपराध के बारे में पर्दापोशी से काम लिया जाए। पश्चिमी सभ्यता का रवैया इसके विपरीत है। वह बुराई के काम में पर्दापोशी से काम नहीं लेती। पश्चिमी धारणाओं के दीवाने यह स्वीकार करने में संकोच करते हैं कि छिपे अपराध की बुराई सीमित रहती है और खुले अपराध के प्रभाव और बुराई पूरे समाज में फैल जाती है।
जब एक बार किसी वजह से बुराई ज़ाहिर हो जाए। ख़ुद से उसको ज़ाहिर करने की अनुमति नहीं है। मुसलमान भाई की ग़लती पर पर्दा डालना चाहिए। अगर किसी से कोई ग़लती हो जाए। किसी के दामन पर कोई धब्बा पड़ जाए, और समाज में किसी को पता न हो। राज्य की संस्थाओं को मालूम न हो। अदालत को पता न हो। एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को उस बुराई के बारे में मालूम हो गया हो तो उसपर पर्दा डालना चाहिए। ग़लती करनेवाले को तौबा की नसीहत करनी चाहिए। आगे से सावधान रहने पर बल देना चाहिए और उसे यह समझाना चाहिए कि अगर इस ग़लती में किसी भाई का ‘हक़’ पाया जाता है तो जाकर चुपके-से अदा कर दो। अगर एक व्यक्ति ने चोरी कर ली और आपकी जानकारी में यह बात आ गई, तो इस्लामी रवैया यह है कि आप उसको समझाएँ कि यह बहुत ग़लत काम किया है। चोरी करना अपराध है। जो चीज़ चुराई है वह जाकर चुपके-से अस्ल मालिक को वापस कर दो। अगर उसको वापस करने में कोई डर या झिझक अवरुद्ध है तो आप किसी और ज़रिये से पहुँचा दें। यह विश्वास कर लें कि मालिक की चीज़ उसको वापस मिल जाए, अल्लाह से तौबा कराएँ और मामले को समाप्त करा दें। किसी से कोई और नैतिक अपराध हो गया हो, या बे-हयाई का जुर्म हो गया। अभी यह मामला किसी के संज्ञान में नहीं आया, कोई उसका गवाह नहीं है। इस मामले को वहीं समाप्त करें, पर्दा डालें और बयान न करें। यह शरीअत का स्वभाव है और यही ‘हया’ का तक़ाज़ा है।
ये अपराध जो हर समाज में होते हैं उनकी संख्या छः है। उनकी सज़ाएँ पवित्र क़ुरआन या हदीसों में बयान की गई हैं। ये सज़ाएँ हर दौर, हर इलाक़े और हर ज़माने के लिए हैं। उनके बारे में यह कहना कि अमुक समाज में यह सज़ाएँ उपयुक्त थीं और अमुक समाज के लिए उपयुक्त नहीं हैं, यह इस्लाम का इनकार करने के समान है। अगर पवित्र क़ुरआन हर दौर के लिए है तो पवित्र क़ुरआन में जो कुछ लिखा है वह भी हर दौर के लिए है। पवित्र क़ुरआन में जहाँ किसी आयत के एक से अधिक अर्थों की गुंजाइश है। इस गुंजाइश का लिहाज़ पवित्र क़ुरआन की आयतों में मौजूद है। शब्दों में और क़ुरआन की भाषा यानी अरबी भाषा में यह सम्भावना और गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात में मौजूद है। लेकिन जहाँ एक से अधिक अर्थों की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ किसी नए इज्तिहाद की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ उस एक ही व्याख्या को अपनाया जाएगा जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने से चली आ रही है।
ताज़ीरी सज़ाओं के दिशानिर्देश
वे अपराध जो हर मानव समाज में नहीं होते, बल्कि कहीं होते हैं और कहीं नहीं होते, उनके बारे में शरीअत ने मौलिक निर्देश दे दिए हैं। इन मौलिक निर्देशों को सामने रखते हुए उस दौर के और इस इलाक़े के बुद्धिवादी और अधिकारी लोग जो उचित सज़ा तय करना चाहें वे तय कर सकते हैं।
इन निर्देशों में जो नियम बताए गए हैं उनमें सबसे पहला नियम यह है कि इस सज़ा का सर्वप्रथम और मौलिक उद्देश्य मुस्लिम समाज और जनसाधारण के जान-माल की रक्षा हो, मात्र किसी एक गिरोह या किसी एक व्यक्ति के हितों की रक्षा न हो। दूसरा उद्देश्य उन सज़ाओं का यह होना चाहिए कि वे निहितार्थ जिनको शरीअत ने स्वीकार किया है, और जो शरीअत में स्वीकार्य हैं, उनमें से किसी उद्देश्य की रक्षा इस सज़ा से पूरी होती हो। तीसरा सिद्धान्त यह है कि इस सज़ा के परिणामस्वरूप इस बुराई के कम होने का सम्भावना हो, पहले के मुक़ाबले में ज़्यादा फैलने की सम्भावना न हो। सज़ा वास्तव में एक शल्य क्रिया यानी ऑप्रेशन है। कुछ बीमारियाँ ऑप्रेशन से समाप्त हो जाती हैं और कुछ ऑप्रेशन से फैल भी सकती हैं। अब यह एक समझदार हकीम का फ़र्ज़ है कि वह देखे कि यह बीमारी फैल जानेवाली है या समाप्त हो जानेवाली है। अगर फैल जानेवाली है तो फिर ऑप्रेशन से काम न ले। इसी तरह सज़ा देने से पहले ये देखना चाहिए कि इस सज़ा के परिणामस्वरूप बुराई समाप्त हो जाएगी या बुराई और बढ़ेगी।
इस हकीमाना अंदाज़ का उदाहरण सीरत में मिलता है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुबारक दौर में कई बार ऐसा हुआ कि मुनाफ़िक़ों ने कुछ आपराधिक हरकतें कीं और मुसलमानों को भारी नुक़्सान पहुँचाया। ऐसे ही एक अपराधी के बारे में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने, ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने दरख़ास्त की कि ऐ अल्लाह के रसूल! इस आदमी को सज़ा-ए-मौत मिलनी चाहिए। अत: मुझे अनुमति दें कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसकी अनुमति नहीं दी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो पूरी दुनिया में यह बात फैलेगी कि मुहम्मद अपने साथियों को क़त्ल करा देते हैं। गोया उस प्रस्तावित सज़ा से तो आपने सैद्धान्तिक रूप से मतभेद नहीं किया, लेकिन व्यवहारतः सज़ा देने से इसलिए गुरेज़ किया कि इससे इस्लाम के बारे में बद-गुमानी फैलेगी। और इससे इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनों को नकारात्मक प्रोपेगंडा करने का जो मौक़ा मिलेगा वह इस बुराई से बहुत बड़ी बुराई होगी जो इस व्यक्ति ने की है।
यह बात मुनाफ़िक़ों (मिथ्याचारियों) के सरदार अबदुल्लाह-बिन-उबई के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कई बार कही। एक बार बनी-मुस्तलक़ के ग़ज़वा में सख़्त गर्मी का ज़माना था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मरीसीअ के स्थान पर अपने अभियान से सफलता के साथ वापस आ रहे थे। इस्लामी सेना ने रास्ते में एक जगह पानी के एक कुएँ के पास पड़ाव किया। बहुत-से लोग पानी लेने के लिए जमा थे। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) अपनी परम्पराओं के अनुसार पंक्ति में क्रम के साथ खड़े थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के एक नौकर जहजाह-बिन-अम्र थे, वे आगे थे उनके पीछे एक वरिष्ठ अंसारी सहाबी भी पानी की प्रतीक्षा में खड़े थे। उनको सम्भवत: नमाज़ के लिए जल्दी थी या इसी तरह की कोई आकस्मिक आवश्यकता थी। जहजाह की बारी आई और वे पानी लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो अंसारी सहाबी ने कहा कि पहले मैं ले लूँ, इसलिए मुझे वुज़ू करने में काफ़ी देर हो गई है। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नौकर को ख़याल हुआ कि क्रम के अनुसार चूँकि पहले मेरी बारी आई है इसलिए पहले मुझे ही पानी लेने का ‘हक़’ है। उन्होंने कुहनी मारकर अंसारी सहाबी को पीछे कर दिया और पानी का डोल अपने हाथ में ले लिया। यह सहाबी इतने बड़े और इतने बुज़ुर्ग सरदारोँ में थे कि जब लोगों ने देखा कि एक नौकर ने उनको कुहनी मारकर पीछे कर दिया है तो उनको बुरा तो महसूस हुआ, लेकिन ख़ामोश रहे। अबदुल्लाह-बिन-उबई मुनाफ़िक़ों का सरदार जो वहाँ खड़ा था, उसने एक दम शोर मचा दिया कि देखो-देखो अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि उनके नौकर भी हमारे प्रतिष्ठित सरदारोँ को कुहनियाँ मारने लगे हैं। फिर उसने कहा कि ज़रा मदीना पहुँचने दो, हममें से जो इज़्ज़तवाला है वह ज़िल्लतवाले को निकाल बाहर करेगा। यह एक लम्बी घटना का हिस्सा है। इससे काफ़ी बदमज़गी पैदा हुई। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बताया कि “ऐ अल्लाह के रसूल! यह बहुत बदतमीज़ आदमी है। यह बार-बार इस तरह की छोटी-छोटी बातों पर हंगामा करने की कोशिश करता है। आप मुझे अनुमति दें कि मैं इसको क़त्ल कर दूँ।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह कहकर मना कर दिया कि “इससे लोग प्रोपेगंडा करेंगे कि मैं अपने साथियों ही को क़त्ल करा देता हूँ।” लोग आम तौर से किसी घटना के वास्तविक कारण की खोज नहीं करते। केवल परिणामों को सरसरी तौर पर देखकर तुरन्त राय क़ायम कर लेते हैं। यहाँ भी ख़तरा था कि सुननेवाले घटना के विवरण और पृष्ठभूमि में नहीं जाएँगे, बल्कि कहा जाएगा कि मुसलमान जिस आदमी को चाहते हैं, मरवा देते हैं इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इन उदाहरणों से यह पता चला कि सज़ा वहाँ दी जाए और उतनी ही दी जाए कि इसके परिणामस्वरूप किसी बड़ी बुराई या किसी बड़े बिगाड़ का ख़तरा न हो, बल्कि यह बिगाड़ या बुराई कम या समाप्त हो जाने का सम्भावना हो।
चौथा सिद्धान्त यह है कि सज़ा और अपराध के दरमियान सन्तुलन हो। यह न हो कि मामूली अपराध पर बहुत बड़ी सज़ा दी जाए और बहुत बड़े अपराध पर मामूली सज़ा दी जाए। एक पड़ोसी देश के बारे में बताया जाता है कि उसमें एक शासक आया। उसने आदेश दिया कि नानबाई जो रोटी बेचते हैं उसका वज़न इतना होना चाहिए। उसके बाद उसने स्वयं जाकर बाज़ार का निरीक्षण किया। एक तन्दूर पर एक रोटी को तुलवाकर देखा, वज़न कम निकला। दूसरी फिर तीसरी और चौथी रोटी तुलवा दी गई तो उनका भी वज़न कम निकला। इस अपराध पर उस शासक ने नानबाई को तन्दूर में डलवाकर ऊपर से तन्दूर बंद कर दिया। जो साहब यह घटना बयान कर रहे थे वह बहुत गर्व से यह बात बयान कर रहे थे। उनका कहना था कि इसके बाद कई वर्ष तक किसी ने कम वज़न की रोटी नहीं बनाई। हो सकता है इसका यह फ़ायदा हुआ हो, लेकिन यह फ़ैसला शरीअत के इस उसूल से मेल नहीं खाता कि अपराध और सज़ा में एक सन्तुलन होना चाहिए। कम वज़न की रोटी बेचना मेरे ख़याल में इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इसपर किसी की जान ले ली जाए।
पाँचवाँ सिद्धान्त यह है कि जो भी ताज़ीरी सज़ा नियुक्त की जाए उसमें सब बराबर हों। सज़ा में किसी छोटे-बड़े का भेदभाव न हो। अपराध कोई भी करे सज़ा उतनी ही दी जाए जो नियुक्त की गई हो।
ये तो अपराध की दृष्टि से दो बड़े-बड़े विभाजन थे। एक प्रकार उन अपराध का था जिनकी सज़ाएँ निर्धारित हैं यानी ‘हुदूद’। दूसरी प्रकार के अपराध वे हैं जिनकी सज़ाएँ निर्धारित नहीं हैं; यानी ‘ताज़ीर’।
इन पाँच सिद्धान्तों को सामने रखते हुए ‘ताज़ीर’ में वर्तमान हुकूमत कोई भी सज़ा निर्धारित कर सकती है। जो सज़ा ‘ताज़ीर’ के बारे में तय की जाएगी। उसमें समय गुज़रने के साथ परिवर्तन, इज़ाफ़ा या कमी भी की जा सकती है। इसको निरस्त भी किया जा सकता है। इन सज़ाओं के मामले में राज्य प्रमुख को माफ़ करने का अधिकार भी प्राप्त है। अलबत्ता ‘हुदूद’ की सज़ा में राज्य प्रमुख को माफ़ करने का अधिकार नहीं। एक और चीज़ जो कम-से-कम हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से चली आ रही है वह यह है कि जो मौलिक सज़ाएँ हैं, जिनको अंग्रेज़ी में capital punishments कहते हैं यानी सज़ा-ए-मौत और अंगों को काटने की सज़ा। ये सज़ाएँ राज्य प्रमुख की अनुमति और सत्यापन के बाद लागू की जाती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह निर्देश जारी किया था कि हाथ काटने और सज़ा-ए-मौत की सज़ाओं पर मेरी मंज़ूरी और सत्यापन के बाद ही अमल किया जाए। उस समय से आज तक यह उसूल चला आ रहा है। अब दुनिया के लगभग हर देश में यह नियम बन गया है कि हर कैपिटल पनिशमेंट राज्य प्रमुख की मंज़ूरी के बाद ही लागू की जाती है। जहाँ तक ‘हुदूद’ के लागू करने का सम्बन्ध है तो राज्य प्रमुख के पास ‘हुदूद’ की सज़ाएँ इस सूचना के लिए भी आती हैं, ताकि वह यह देख सके कि यह सज़ा सही तौर पर दी गई है, क्या सचमुच यह व्यक्ति इस सज़ा का पात्र था। सज़ा देने में शरीअत और क़ानून के तमाम तक़ाज़े सामने रखे गए हैं। अगर वह इसपर सन्तुष्ट हो जाए तो फिर वह अनिवार्य रूप से सज़ा का सत्यापन करेगा। उसे कोई अधिकार नहीं है कि उसको माफ़ करे। पाकिस्तान में भी यही क़ानून है। अगरचे इस्लामी लोकतंत्र पाकिस्तान के आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि किसी भी अदालत से मिलनेवाली सज़ा को कम करने, बदलने या बिलकुल समाप्त करने का अधिकार पाकिस्तान के राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ उच्च न्यायालयों का फ़ैसला भी है और आज से लगभग बीस वर्ष पहले का एक राष्ट्रपति आदेश भी है। इस आदेश के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 1979 से लेकर आज तक ‘हद’ की कोई सज़ा समाप्त नहीं की। ‘क़िसास’ की सज़ा भी समाप्त नहीं की, क्योंकि उसमें माफ़ करने का ‘हक़’ प्रभावित व्यक्तियों का है। वे चाहें यानी क़त्ल किए गए व्यक्ति के वारिस लोग चाहें तो माफ़ कर दें और न चाहें तो माफ़ न करें। लेकिन ‘हुदूद’ और ‘क़िसास’ के अलावा शेष तमाम मामलों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आर्टिकल 45 के तहत अधिकार प्राप्त है कि सज़ा को माफ़, समाप्त या कम कर दे। उनमें ‘ताज़ीर’ की सज़ाएँ भी शामिल हैं।
‘ताज़ीर’ की मात्रा का निर्धारण
‘ताज़ीर’ की सज़ा के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक और महत्वपूर्ण और मौलिक हिदायत दी है जिसके बारे में फ़ुक़हा के बारे में थोड़ा-सा मतभेद भी पाया जाता है। चूँकि महत्वपूर्ण बात है इसलिए अर्ज़ कर देता हूँ। हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह फ़रमाया कि “ताज़ीर की सज़ा हद की सज़ा के बराबर नहीं होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हद के अलावा किसी अपराध में हद के बराबर सज़ा दी तो वह ज़्यादती करनेवालों में से है।” इस सिद्धान्त पर सब इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) का मतैक्य है। इस मामले में फ़िक़ही मसलकों में कोई मतभेद नहीं कि कोई ताज़ीरी सज़ा हद की सज़ा के बराबर नहीं होगी। इस सीमा तक सैद्धान्तिक मतैक्य के बावजूद इस बात में मतभेद है कि इससे मुराद क्या है? कुछ लोगों का यह कहना है और मुझे यही राय दुरुस्त मालूम होती है कि किसी ऐसे अपराध में जिसमें शरीअत ने हद की सज़ा दी हो, अगर कोई व्यक्ति इस बड़े अपराध से छोटा कोई अपराध करे तो इस छोटे अपराध में उसको हद के बराबर सज़ा न दी जाए। उदाहरण के रूप में शरीअत में शराबनोशी की सज़ा 80 कोड़े है। अब ज़ाहिर है कि यह सज़ा शराब पीने की है। शराब पीने से कम के किसी अपराध की नहीं है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति शराब नहीं पी रहा था, लेकिन शराब की बोतल बग़ल में दबाए जा रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया। अब शराब की बोतल क़ब्ज़े में रखना अस्ल अपराध से कम है। पी नहीं, लेकिन हाथ में है। इसकी सज़ा 80 कोड़े नहीं होगी। इसी तरह किसी व्यक्ति ने अभी चोरी की नहीं, लेकिन चोरी की नीयत से खड़ा था या ताला तोड़ने की योजना बना रहा था। अगर यह आदमी चोरी कर लेता तो उसकी सज़ा ‘हाथ काटना’ होती। लेकिन चोरी की कोशिश, नीयत या ताला तोड़ने की सज़ा तो ‘हाथ काटना’ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़याल में इस हदीस से यही मुराद है।
कुछ और फ़ुक़हा का कहना है कि दुनिया के किसी भी अपराध में उसकी सज़ा हद की कम-से-कम सज़ा से कम होनी चाहिए। हद की कम-से-कम सज़ा चालीस कोड़े है। शराब पीने और क़ज़्फ़ की अस्ल सज़ा तो अस्सी कोड़े है, लेकिन ग़ुलामों को आधी सज़ा दी जाती थी इसलिए उनकी सज़ा चालीस कोड़े क़रार दी गई थी। चूँकि उस ज़माने में ग़ुलामों के अधिकार कम थे इसलिए उनकी सज़ा भी कम होती थी। अत: अस्सी कोड़ों की बजाय उनको चालीस कोड़ों की सज़ा मिलती थी। इसलिए गोया कम-से-कम सज़ा में चालीस कोड़े सज़ा की आख़िरी हद है। इसलिए उन लोगों की राय में ‘ताज़ीर’ की ज़्यादा-से-ज़्यादा सज़ा उनतालिस (39) कोड़े होने चाहिएँ। इन फ़ुक़हा का कहना यह है कि कोई अपराध हो, उसका प्रकार कुछ भी हो, उसकी ताज़ीरी सज़ा 39 कोड़ों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़ुक़हा में कुछ लोगों का यही ख़याल है। ये दोनों दृष्टिकोण ताज़ीर की सज़ा के बारे में पाए जाते हैं। पहले दृष्टिकोण का समर्थन कई घटनाओं और हदीसों से होता है। जिनसे पता चलता है कि पहली ही बात ज़्यादा दुरुस्त है। उदाहरण के रूप में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में एक व्यक्ति ने बैतुलमाल की जाली मुह्र बना ली और हर तीसरे-चौथे महीने एक जाली आर्डर पर मुह्र लगाकर बैतुलमाल से पैसे जारी करवाता था। बहुत दिनों के बाद सम्भवत: वर्ष के समाप्त होने पर जब हिसाब होने लगा तो पता चला कि बैतुलमाल से रक़म इन ख़र्चों से ज़्यादा निकाली गई जितने ख़र्चे मंज़ूर हुए थे। अब जब चेक किया गया तो चार पाँच जाली दस्तावेज़ात निकलीं। और अधिक पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि यह साहब इसमें लिप्त हैं। मामला हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सेवा में पेश किया गया। उन्होंने फ़रमाया कि इसको सौ कोड़े लगवाओ। इस आदमी को सौ कोड़े लगाए गए। अगले दिन उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा कि कहाँ है। उसको दोबारा सेवा में हाज़िर किया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने महसूस किया कि इस व्यक्ति को अभी तक अपनी ग़लती के बारे में कुछ ख़ास पछतावा नहीं है। दोबारा सौ कोड़े लगवाने का आदेश दिया और इसपर अमल हुआ। फिर तीसरे दिन बुलाया और बातचीत की तो अनुमान हुआ कि यह आदमी अभी तक अपने रवैये पर शर्मिन्दा नहीं है, और ख़तरा है कि दोबारा इस काम को करे। कुछ अपराधी बहुत सख़्त होते हैं। इसलिए इस आदमी को तीन दिन सौ-सौ कोड़े लगाए गए। चौथे दिन जब बुलाया तो अनुमान हुआ कि अब यह आदमी बाज़ आने का इरादा रखता है और कहता है कि आइन्दा ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसको समझा-बुझाकर और नसीहत करके रुख़स्त कर दिया। इस तरह की कई एक और घटनाएँ भी हैं जिनसे पता चलता है कि कोड़ों की सज़ा उनतालीस कोड़ों से ज़्यादा भी हो सकती है, बल्कि तीन सौ कोड़े भी हो सकते हैं।
ताज़ीर की सज़ा के बारे में एक मौलिक सिद्धान्त और भी है। वह यह है कि जब किसी अपराध की सज़ा नियुक्त की जाए तो दो चीज़ें सामने रखी जाएँ। सबसे पहली चीज़ तो यह देखी जाएगी कि जिस चीज़ को आप अपराध क़रार दे रहे हैं क्या वह अल्लाह की शरीअत में पहले से नापसंदीदा है और नाजायज़ है। अगर पहले से नाजायज़ है तो उसके लिए केवल सज़ा नियुक्त कर देना काफ़ी है। इसको नए सिरे से अपराध क़रार देने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो पहले उसको विधिवत रूप से अपराध क़रार दे दें और चाहें तो पूर्व शरीअत के आदेशों ही को काफ़ी क़रार दें और नए सिरे से विधिवत रूप से अपराध क़रार न दें। वह तो पहले ही अपराध है। अगर वह कार्य पहले से अल्लाह की शरीअत में अपराध नहीं था और आज आपने किसी ‘मस्लहत’ के आधार पर उसको अपराध क़रार दिया है, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप पहले यह एलान करें कि आज से अमुक कार्य अपराध है और आज के बाद इस काम की अनुमति नहीं है। जब लोगों को उसके अपराध होने का अच्छी तरह पता चल जाए और उन्हें मालूम हो जाए कि आज से अमुक काम अपराध है और नापसंदीदा है। फिर उसकी सज़ा दी जाए। लोगों की सूचना और शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बिना किसी कार्य को अपराध क़रार देना और अचानक कोड़ा लेकर उनकी कमर पर बरसा देना शरीअत में जायज़ नहीं है।
प्रतिष्ठित फ़ुक़हा ने पवित्र क़ुरआन की बहुत-सी आयतों से इस सिद्धान्त को निकाला है। उदाहरण के रूप में एक जगह आया है कि “हम किसी को उस समय तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक हमने पहले वहाँ रसूल न भेजा हो।” (क़ुरआन, 17:15) जिस क़ौम में पैग़ंबर या रसूल नहीं आया उस क़ौम से उन अपराध के बारे में पूछ-गछ नहीं की जाएगी। जो अपराध पैग़म्बरों की शिक्षा के परिणामस्वरूप मालूम हुए हों कि ये अपराध हैं, जिनका बुरा या अनैतिक होना अल्लाह की वह्य से मालूम हुआ, उनको वह्य (ईश-प्रकाशना) के अवतरण से पहले करने पर सज़ा नहीं दी जाएगी।
एक जगह आया है कि “तेरा रब तो बस्तियों को विनष्ट करनेवाला नहीं जब तक कि उनकी केन्द्रीय बस्ती में कोई रसूल न भेज दे।” (क़ुरआन, 28:59) अल्लाह किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा जब तक यह सारी प्रक्रिया पूरी न हो जाए। पहले उसमें नबी को भेजा जाएगा, रसूल को भेजा जाएगा, वह शिक्षा देगा, प्रशिक्षण करेगा। फिर अगर ग़लती होगी तो सर्वोच्च अल्लाह सज़ा देगा। अल्लाह ने यह फ़ैसला स्वयं अपने बारे में भी नहीं किया। हालाँकि वह जानता है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है। अगर वह यह कहता कि मैं जानता हूँ कौन अपराधी है और कौन नहीं है तो यह बात आसानी से मान ली जाती, लेकिन उसने यह चीज़ अपने अधिकार में भी नहीं रखी। किसी व्यक्ति के अपराधी ठहराए जाने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे अपनी सफ़ाई का पूरा मौक़ा दिया जाए और एक खुली अदालत में दोनों पक्षों के गवाह सामने लाए जाएँ। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इरशाद है जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बयान किया। कुछ लोगों के ख़याल के अनुसार यह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अपना कथन है। मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) में यह हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के कथन के तौर पर बयान किया गया है कि “इस्लाम में किसी व्यक्ति को बिना न्यायप्रिय गवाहों और बिना न्यायिक प्रक्रिया के क़ैद की सज़ा नहीं दी जाएगी।” यह विधि पूरे तौर पर अपनाई जाएगी। सर्वोच्च अल्लाह ने यह चीज़ अपने ज़िम्मे रखी है। क़ियामत के दिन वह कह सकता है कि ऐ अमुक, मैं जानता था कि तू बदकार और अपराधी है अत: जा तू जहन्नम में चला जा। सर्वोच्च अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। सर्वोच्च अल्लाह ने वे तमाम गवाहियाँ तैयार कर रखी हैं जो इंसान इस दुनिया में किसी अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए तैयार किया करता है। इंसान यहाँ अपना दावा साबित करने और अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए चश्मदीद गवाह लाता है। दस्तावेज़ी गवाहियाँ लाता है, circumstantial evidence यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की दलीलें लाता है। लोगों के हलफ़िया बयान लाता है। क्षतिग्रस्त पक्ष के बयान लाए जाते हैं। सर्वोच्च अल्लाह ने यह सारे तर्क और सुबूत तैयार किए हैं। वहाँ दो चश्मदीद गवाह भी होंगे। दस्तावेज़ी सुबूत भी होंगे circumstantial evidence भी होगा। विरोधी पक्ष के अपने गवाह अगर अपने ख़िलाफ़ ही गवाही दे दें तो आपका मुक़द्दमा तुरन्त निबट जाता है। आपका अगर किसी के साथ मतभेद हो कि अमुक के ज़िम्मे आपके एक लाख रुपये बाक़ी हैं। वह न मानता हो और उसका अपना बेटा या उसकी अपनी पत्नी खड़े होकर गवाही दे दें कि जी वाक़ई यह दावा दुरुस्त है और उन साहब के एक लाख रुपये मेरे पिता या पति के ज़िम्मे बाक़ी हैं तो अदालत तुरन्त फ़ैसला कर देगी और वह व्यक्ति ख़ामोश हो जाएगा कि इसके अपनों ने गवाही दे दी है। अत: अगर इंसान के अपने ही शरीर के अंग गवाही दे दें कि उनसे यह अपराध कराया गया था तो फिर इंसान कुछ कहने की पोज़ीशन में नहीं रहेगा। जब सर्वोच्च अल्लाह ने अपने लिए यह सारी प्रक्रिया रखी है कि एक खुली अदालत में तमाम इंसानों के सामने एक-एक चीज़ साबित करने के बाद फ़ैसला किया जाएगा तो इंसानों को क्या ‘हक़’ पहुँचता है कि वह अपने अत्यन्त सीमित ज्ञान, सीमित अन्तर्दृष्टि और सीमित बुद्धि से काम लेकर जिसको चाहें सज़ा दे दें और जिसको चाहें मुक्त कर दें।
‘ताज़ीर’ के लिए कोई निर्धारित सज़ा नहीं है। ताज़ीर के तौर पर वर्तमान हुकूमत या क़ानून बनानेवाली संस्था जो भी सज़ा तय करना चाहे कर सकती है। इसमें संक्षिप्त क़ैद की सज़ा भी हो सकती है। इसमें मामूली मार की सज़ा भी हो सकती है, कोड़ों की सज़ा भी हो सकती है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है। जो सज़ा उचित हो और वह इस अपराध से मेल खाती हो, वह दी जा सकती है। अगर यह महसूस हो कि इस सज़ा से अपराध को समाप्त करने में मदद मिल रही है तो वह सज़ा शेष रहेगी। और अगर यह ख़याल हो कि यह सज़ा काफ़ी नहीं है तो उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यह भी तय किया जा सकता है कि अगर एक या दो या तीन बार इस अपराध को किया जाए तो सज़ा नहीं मिलेगी और तीसरी या चौथी बार अपराध को किया जाएगा तो फिर सज़ा मिलेगी। इस तरह से यह सारा विवरण तय करने का पूरा अधिकार क़ानून बनानेवाली शक्ति को है।
पहली प्रकार के क़ानून वे हैं जो ‘हुदूद’ के क़ानून कहलाते हैं। और ये पाकिस्तान में 10 फ़रवरी 1979 को लागू हुए थे। 10 फ़रवरी 1979 को पाँच क़ानून लागू किए गए थे जिनमें चोरी, हराबा, शराबनोशी, बदकारी और क़ज़्फ़ (झूठा आरोप) की सज़ाएँ शामिल हैं। इन पाँच सज़ाओं में फ़ुक़हा के दरमियान थोड़ा-सा मतभेद है कि किन मामलात में और किन अपराध में हुकूमत या अदालत को ख़ुद से कार्रवाई करने का अधिकार है, किन मामलात में किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर भी कार्रवाई करने का अधिकार है जो ख़ुद से इस मामले से प्रभावित या क्षतिग्रस्त पक्ष यानी aggrieved पार्टी न हो। और किन मामलात में क्षतिग्रस्त या नुक़सान उठानेवाले पक्ष का स्वयं सामने आना ज़रूरी है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) का कथन यह है कि जो मामलात सौ प्रतिशत ‘हुक़ूक़ुल-इबाद’ के प्रकार के हैं या जिनमें बंदों के अधिकार प्रभावी हैं उनमें प्रभावित पक्ष का अदालत में स्वयं आना ज़रूरी है। बिना मूल प्रभावित के किसी और के कहने पर मुक़द्दमा दर्ज नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया। तो जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया है वह, या उसका वली (संरक्षक) या उसका वारिस स्वयं आकर शिकायत करेगा तो मुक़द्दमा शुरू होगा, वरना मुक़द्दमा शुरू नहीं होगा। क़ज़्फ़ के मामले में इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) का यही दृष्टिकोण है। जिन मामलों में बन्दे का अधिकार प्रभावी है, उदाहरणार्थ क़िसास, उसमें सब फ़ुक़हा का मतैक्य है कि क़िसास की माँग के लिए पीड़ित व्यक्ति का आना ज़रूरी है, सिवाय यह कि क़त्ल की घटना ऐसे ढंग से हुई हो कि इससे पूरे समाज में terror या आतंक फैल गया हो या जहाँ ताज़ीर सज़ा-ए-मौत देना ज़रूरी हो तो वहाँ राज्य को सीधे हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। यह विस्तृत विवरण हैं जो उलमा किराम ने बयान किए हैं।
क़िसास की धारणा
जहाँ तक क़िसास का सम्बन्ध है यह ‘हुदूद’ से किसी हद तक विभिन्न और किसी हद तक ‘हुदूद’ के समान एक विषय है। इस दृष्टि से इसका मामला ‘हुदूद’ जैसा है कि क़िसास की सज़ा सर्वोच्च अल्लाह ने निर्धारित की है। पवित्र क़ुरआन में आया है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। इस हद तक यह सज़ा निर्धारित है। इसमें किसी संशोधन या कमी-बेशी की गुंजाइश नहीं। लेकिन एक-दूसरे पहलू से यह चीज़ हद से भिन्न है और ताज़ीरात से मिलती-जुलती है, वह यह है कि ताज़ीर की तरह क़िसास में भी सज़ा में कमी-बेशी हो सकती है। यहाँ हाकिम के विपरीत पक्ष ‘मुतज़र्रर’ (क्षतिग्रस्त पक्ष) को माफ़ कर देने का अधिकार है। यों एक तरह से क़िसास ‘हुदूद’ और ताज़ीर दोनों का विशिष्टता combination है। उनमें कुछ विशेषताएँ ‘हुदूद’ की और कुछ ताज़ीर की पाई जाती हैं। इसलिए फ़ुक़हा की बड़ी संख्या ने क़िसास को ‘हुदूद’ की सूची से अलग रखा है। क़िसास एक अलग विषय है और इसके अलग नियम हैं। क़िसास के शाब्दिक अर्थ तो बड़े दिलचस्प हैं, यानी किसी के पदचिह्नों पर क़दम रखकर चलना। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा हो और उसके क़दमों के निशान रेत पर पड़ रहे हों। आप उन निशानात पर पाँव रखकर चलते जाएँ तो इस क्रिया को अरबी भाषा में ‘क़िसास’ कहते हैं। इस क्रिया में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। वह यह कि जैसा अस्ल नक़्श था उसी के अनुसार आपने पाँव रखा, अंगूठे की जगह अँगूठा, उंगली की जगह उंगली और तलवे की जगह तलवा आ जाए। इसको ‘क़िसास’ कहेंगे। गोया दो चीज़ों के एक-दूसरे से पूर्ण रूप से समान होने की क्रिया को अरबी भाषा में क़िसास कहते हैं। चूँकि क़िसास का कलात्मक अर्थ भी यही है कि जैसा अपराध हुआ था उसी तरह का कृत्य अपराधी के साथ किया जाए। इसलिए इस कार्य को क़िसास कहते हैं। क़िसास के मामले में एक चीज़ याद रखने की है। इंसानी जान के ख़िलाफ़ जितने भी अपराध हैं उनकी दो क़िस्में हैं। क़िसास इंसानी जान के ख़िलाफ़ अपराध में होता है किसी और चीज़ के ख़िलाफ़ अपराध में नहीं होता। माल के ख़िलाफ़, इज़्ज़त के ख़िलाफ़ या समाज के ख़िलाफ़ अपराध में क़िसास नहीं होगा। केवल जान के ख़िलाफ़ अपराध में क़िसास होगा। इसलिए इन अपराधों को ‘जिनायतु अलन-नफ़्स’, भी कहते हैं। किसी की जान के ख़िलाफ़ कोई अपराध हुआ है तो उसके दो प्रकार हैं। कुछ अपराध तो वे हैं कि आप इन अपराधों के करनेवालों को वैसी ही सज़ा दे सकते हैं और पूरी समानता के साथ दे सकते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे को क़त्ल कर दिया। आप क़िसास में उसको क़त्ल कर दें। उसने पहले की जान नष्ट की थी आप सज़ा के तौर पर उसकी जान नष्ट कर दें। इस सज़ा में बिलकुल और पूरी समानता सम्भव है। जान के बर्बाद होने में समानता सम्भव है। इसी तरह कुछ ज़ख़्मों में भी समानता सम्भव है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने किसी का कान काट दिया, क़िसास में उसका कान काट दिया जाएगा। अत: जिन मामलात में मूल अपराध और सज़ा के बीच समानता सम्भव है वहाँ शरीअत ने क़िसास का आदेश दिया है। जहाँ पूरी समानता सम्भव नहीं है वहाँ शरीअत ने क़िसास की अनुमति नहीं दी है, वहाँ ‘दियत’ का आदेश दिया है। ‘दियत’ का विवरण हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। उनका विवरण अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं बयान किया हैं। उनको आपने किसी फ़क़ीह के इज्तिहाद या समझ पर नहीं छोड़ा। बहुत-सी हदीसें हैं जिनमें एक ही बात बयान हुई है।
वे अपराध जिनमें पूरी समानता के साथ क़िसास सम्भव न हो, उनके फिर और दो प्रकार हैं। एक प्रकार वह है जिसका प्रभाव इंसान के सिर पर हो। दूसरा प्रकार वह है जिसका प्रभाव इंसानी जिस्म के शेष किसी हिस्से पर हो। सिर पर प्रभावी होनेवाले अपराध के लिए हदीस में ‘शज्जह’ की शब्दावली आई है और फ़िक़्हे-इस्लामी की किताबों में भी यही शब्दावली प्रयुक्त हुई है। शज्जह का बहुवचन है ‘शिजाज’। सिर में जो ज़ख़्म होते हैं उनका अत्यन्त बारीक और साइंटिफ़िक और बड़ा minute (सूक्ष्म) विवरण हदीसों में आया हैं। एक बार मुझे एक पश्चिमी अपराध विशेषज्ञ के सामने शिजाज का यह विवरण बयान करने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। उन्होंने इसपर असाधारण आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि क्या वाक़ई चौदह सौ वर्ष पहले यह विवरण मौजूद था? मैंने कहा कि जी बिलकुल मौजूद था। हमारे यहाँ कुछ अयोग्य, नालायक़ और जाहिल लोग (ये शब्द सख़्त हैं लेकिन मैं अत्यन्त ज़िम्मेदारी के साथ इनको प्रयुक्त कर रहा हूँ) मैंने बहुत-से ऐसे आदमियों से सुना है कि वे इन चीज़ों को (अल्लाह की पनाह) फ़ुज़ूल और अव्यावहारिक क़रार देते हैं। यह इंसान का अत्यन्त दुर्भाग्य होता है और उसकी तबाही और पतन की एक दलील होती है कि उसको न नेमत का पता चले कि यह नेमत है और न पतन का पता चले कि यह पतन है।
‘शज्जह’ के कुल दस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार वह है जिसमें सिर की खाल कट जाए लेकिन ख़ून न बहे। तमाम प्रकारों के नाम भी अलग-अलग हैं, लेकिन मैं नाम लेकर आपपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। किसी व्यक्ति ने तलवार या छुरी या डंडा किसी के सिर पर मारा। वह सिर के किसी हिस्से पर लगा और सिर के प्रभावित हिस्से की खाल फट गई। अब ज़ाहिर है यह नहीं हो सकता कि आप किसी के सिर पर प्रत्युत्तर में इसी तरह चोट लगाएँ कि उसकी केवल खाल तो फट जाए और उससे ज़्यादा नुक़्सान न हो। हो सकता है कि जब उसने छुरी मारी थी तो किसी वजह से चोट ज़ोर से नहीं लगी। केवल खाल कट गई। अब यह नहीं हो सकता कि आप उसको ऐसी ही चोट लगाएँ कि उसकी भी खाल फटे। हो सकता है ज़्यादा कट जाए। हो सकता है न कटे। दोबारा अगर मारेंगे तो यह ज़्यादती होगी। इसलिए इसमें समानता सम्भव नहीं है। इसकी शरीअत ने ‘दियत’ नियुक्त की है।
दूसरा दर्जा यह है कि खाल भी कट जाए और ख़ून भी निकल आए। तीसरा दर्जा यह है कि अन्दर का गोश्त भी कट जाए। चौथा दर्जा यह है कि हड्डी नज़र आने लगे। पाँचवाँ दर्जा यह है कि हड्डी में क्रेश पड़ जाए। छटा दर्जा यह है कि हड्डी टूट जाए और दिमाग़ नज़र आने लगे। आख़िरी दर्जा यह है कि दिमाग़ बाहर निकल आए। चोट या ज़रब अस्ल दिमाग़ तक पहुँच जाए। इन सबकी ‘दियत’ के अलग-अलग आदेश हैं और सब हदीसों में बयान हुए हैं। किसमें क्या तत्वदर्शिता है, कभी-कभी तत्वदर्शिता समझ में आती है और कभी-कभी समझ में नहीं आती। जहाँ कोई तत्वदर्शिता समझ में न आए उसमें इंसान को अपनी बुद्धि की कमी को स्वीकार करना चाहिए।
जो ज़ख़्म जिस्म के शेष किसी हिस्से पर हों, उनके फिर दो प्रकार हैं। एक को ‘जाइफ़ा’ और दूसरे को ‘ग़ैर-जाइफ़ा’ कहते हैं। जाइफ़ा का अर्थ है वह ज़ख़्म जो जिस्म के ऊपरी हिस्से, यानी धड़ के अन्दर तक हो जाए। यानी वह हिस्सा जिसमें इंसान का जिगर, मेदा (यकृत), पेट आदि शामिल हैं। किसी ने तलवार किसी के पेट में घोंप दी। उसके जिगर तक चली गई या मेदे के अन्दर तक चली गई तो यह जाइफ़ा है। दूसरी शक्ल यह है कि तलवार अन्दर तक नहीं गई। पिंडली में लग गई या किसी और जगह लग गई, गोश्त फट गया, लेकिन अन्दर नहीं गया। इन सबमें सबकी दियतें अलग-अलग निर्धारित हैं।
कुछ जगह ऐसा ज़ख़्म हो सकता है कि वह इन बयान किए गए प्रकारों में से किसी भी प्रकार में न आता हो। सम्भव है कि उनमें उप विवरण इतने बारीक हों कि दो ज़ख़्मों को आप एक सतह पर न रख सकें। एक व्यक्ति ने लोहे की एक रॉड लेकर तीन आदमियों की पिंडलियों पर ज़ोर से मारी। तीनों का ज़ख़्म भिन्न हो सकता है। जब चिकित्सा विशेषज्ञ ने देखा तो तीनों ज़ख़्मों के dimensions और quantity भिन्न थीं। सवाल यह है कि अब क्या करें। अगर तीनों को एक तरह की ‘दियत’ दिलाएँ तो यह इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है। जब ज़ख़्म और चोट का प्रकार अलग-अलग है तो ‘दियत’ एक क्यों हो। यहाँ शरीअत ने एक शब्दावली प्रयुक्त की है हुकूमते-अद्ल। हुकूमत का अर्थ फ़ैसला और अद्ल का मतलब अद्ल करनेवाला या इंसाफ़ करनेवाला, जो ज़ख़्मों का माहिर हो यानी ऐसा जर्राह या सर्जन जो न्यायप्रिय और इंसाफ़-पसन्द स्वभाव रखता हो वह इन तीनों ज़ख़्मों का निरीक्षण करे और यह बताए कि किसका ज़ख़्म किस प्रकार और कैफ़ियत का है और शरीअत के इन आम निर्देशों के अनुसार उस ज़ख़्म की ‘दियत’ कितनी होनी चाहिए। जो ‘दियत’ वह क़रार दे वह ‘दियत’ आप अदा कर दें।
यह उन आदेशों का अति संक्षिप्त सार है जो शरीअत ने क़िसास के बारे में दिए हैं। क़िसास के आदेश पाकिस्तान में 1990 से लागू हैं।
क़त्ल के प्रकार
क़िसास के मामले में जहाँ तक क़त्ल का सम्बन्ध है, इसके अनेक प्रकार अब दुनिया के लगभग तमाम क़ानून स्वीकार करते हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों के ज्ञान में है कि क़त्ल के भिन्न प्रकारों के बीच यह सूक्ष्म अन्तर और उन सब प्रकारों के अलग-अलग विस्तृत आदेश इस्लामी शरीअत की देन हैं। शरीअत से पहले दुनिया के क़ानून क़त्ल के इतनी सूक्ष्म विवरण से अवगत नहीं थे।
क़त्ले-अमद (जान-बूझकर किया गया क़त्ल)
क़त्ल के तीन प्रकारों पर तो तमाम फ़ुक़हा सहमत हैं। एक क़त्ले-अमद (जान-बूझकर किया जानेवाला क़त्ल) है। क़त्ल-अमद वह है जिसमें कोई व्यक्ति जान-बूझकर क़त्ल करने के इरादे से किसी हथियार की सहायता से किसी बेगुनाह व्यक्ति को क़त्ल कर दे। यानी किसी व्यक्ति की नीयत भी मुजरिमाना हो। वह दूसरे व्यक्ति को भारी नुक़्सान पहुँचाना भी चाहता हो और ऐसा हथियार प्रयुक्त करे जो क़त्ल के हथियार के तौर पर शुमार किया जा सकता हो। जब ये तीन शर्तें मौजूद होंगी तो उसको क़त्ले-अमद क़रार दिया जाएगा।
क़त्ले-शुब्हे-अमद (हत्या के इरादे का सन्देह)
दूसरा प्रकार है क़त्ले-शुब्हे-अमद। यह क़त्ले-अमद से मिलता जुलता है। वह यह है कि किसी व्यक्ति की नीयत तो दूसरे को क़त्ल करने की नहीं थी, बल्कि मात्र उसको चोट पहुँचाना या ज़ख़्मी करना चाहता था या मात्र मार-पीट करना चाहता था, उसने क़त्ल का हथियार भी प्रयुक्त नहीं किया। और जो औज़ार इस काम के लिए प्रयुक्त किया उस औज़ार से आम तौर पर आदमी मरता नहीं है, लेकिन संयोगवश उसकी इस चोट से वह व्यक्ति मर गया। यानी एक व्यक्ति दूसरे को मारना-पीटना तो चाहता था। नीयत भी आपराधिक थी, लेकिन क़त्ल कर डालना उसका उद्देश्य नहीं था, उसने सिर पर डंडा मारा। अब डंडे से कोई किसी को क़त्ल नहीं करता। डंडा आम तौर पर क़त्ल के लिए प्रयुक्त नहीं होता। लेकिन डंडा सिर पर या जिस्म के किसी नाज़ुक हिस्से पर इस तरह मारा कि आदमी मर गया। यह शुब्हे-अमद है। ये क़त्ले-अमद से एक दर्जा कम है।
क़त्ले-ख़ता (भूल से हुई हत्या)
तीसरा प्रकार क़त्ले-ख़ता का है कि इंसान की नीयत बिलकुल बुरी नहीं थी। न वह मारना चाहता था। न वह नुक़्सान पहुँचाना चाहता था न ही उसके ज़ेहन में कोई बुरा इरादा था, लेकिन किसी ग़लती की वजह से किसी इंसान की जान चली गई। ग़लती तीन प्रकार की हो सकती है। एक ग़लती कार्य में हो सकती है। एक ग़लती लक्ष्य में हो सकती है और एक ग़लती इरादे में हो सकती है। कार्य की ग़लती यह है कि उदाहरणार्थ आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं, उसके पीछे कोई आदमी सो रहा था। आपने गाड़ी रिवर्स की तो वह आदमी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। आपकी नीयत उसको नुक़्सान पहुँचाने की बिलकुल नहीं थी, लेकिन एक कार्य आपने ऐसा किया कि उसके परिणामस्वरूप एक बेगुनाह व्यक्ति मर गया। यह क़त्ले-ख़ता है। एक ग़लती इरादे की हो सकती है। उदाहरणार्थ आप शिकार पर गए हैं और दूर से आपने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बत्तख़ है। आपने गोली चला दी। क़रीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वह बत्तख़ नहीं थी, बल्कि कोई आदमी था जो सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। दूर से आपको बत्तख़ लगी। अब आपने हमला तो इसपर किया था और इसी को निशाना भी बनाया, लेकिन आपकी नीयत यह नहीं थी कि आप किसी इंसान को मार दें, बल्कि आप तो बत्तख़ को मारना चाहते थे। यह ग़लती का एक और प्रकार है और यह लक्ष्य की ग़लती है। एक ग़लती यह है कि आपने गोली वाक़ई जानवर पर चलाई थी। परिंदा बैठा हुआ था। किसी वजह से आपका हाथ चूक गया और बराबर में खड़े किसी इंसान को लग गई। मैदाने-जंग में किसी दुश्मन फ़ौजी पर गोली चलाई थी, लेकिन वह ग़लती से किसी मुसलमान सिपाही को लग गई। हनफ़ी आलिमों ने इनके अलावा भी क़त्ल के और दो प्रकार बयान किए हैं यानी क़त्ले-क़ाइम मक़ाम ख़ता और क़त्ले-बित्तसब्बुब। दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक ये दोनों क़त्ले-ख़ता ही के प्रकार हैं।
शरीअत ने क़त्ल के इन तीनों प्रकारों की सज़ाएँ अलग-अलग रखी हैं। ‘क़िसास’ की सज़ा केवल क़त्ले-अमद पर है। इसमें मक़्तूल के वारिसों को माफ़ करने का अधिकार है। क़त्ले-शुब्हे-अमद की सज़ा ‘दियत’ है। वह व्यक्ति जिससे ग़लती हुई है वह उसकी ‘दियत’ अदा करेगा। पवित्र क़ुरआन की सूरा-4 निसा में विस्तृत आदेश मौजूद हैं। आप क़ुरआन की किसी उचित टीका की सहायता से इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा।
‘दियत’ के ज़रूरी आदेश
‘दियत’ के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो निर्देश दिए थे वे ये हैं कि या तो सौ ऊँट अदा किए जाएँ, या बारह हज़ार दिरहम चांदी के अदा किए जाएँ, या सोने के एक हज़ार सिक्के (दीनार) अदा किए जाएँ। उस ज़माने में इन तीनों की मालियत लगभग बराबर-बराबर थी। बाद में मालियत में कमी-बेशी आ गई। जब कमी-बेशी आ गई तो फ़ुक़हा में यह सवाल पैदा हुआ कि उनमें अस्ल किसको समझा जाए। कुछ फ़ुक़हा का, जिनमें इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) शामिल हैं, यह कहना है कि अस्ल ऊँट को समझा जाएगा। चुनाँचे सऊदी अरब में आज ‘दियत’ की जो रक़म है वह ऊँट की मार्केट वैल्यू के अनुसार चुकाई जाती है। वहाँ का न्याय मंत्रालय हर दो-तीन वर्ष के बाद सौ ऊँटों की मालियत का निर्धारण कर देता है और यह एलान कर देता है कि अब मार्केट में ऊँट की क़ीमत इतनी है और इस हिसाब से ‘दियत’ की रक़म इतनी है। इसलिए कि हदीस में ऊँट ही का ज़िक्र अधिक महत्वपूर्ण तरीक़े से है।
कुछ दूसरे फ़ुक़हा का कहना है कि सोने को अस्ल समझा जाएगा। जबकि कुछ का ख़याल है कि चाँदी को अस्ल समझा जाएगा। जब पाकिस्तान में 1990 में यह क़ानून बन रहा था। उस समय मैं भी इस्लामी वैचारिक परिषद का सदस्य था। मेरा कहना यह था कि आज के दौर में ‘दियत’ की मालियत के निर्धारण में सोने को असल माना जाए। इसलिए कि सोना वास्तविक धन (ज़र) है। हर ज़माने में धन रहा है, आज भी धन है और सुदूर भविष्य तक ज़रूर रहेगा। चाँदी के धन होने की हैसियत अब लगभग समाप्त हो गई है। अब चाँदी धन नहीं रही। और चाँदी की मालियत सोने के मुक़ाबले में दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। जो अनुपात या ratio आज से उदाहरणार्थ सौ वर्ष पहले सोने और चाँदी में था, आज इस हिसाब से यह अनुपात दस प्रतिशत भी नहीं रहा। इससे पहले इन दोनों के दरमियान जो सम्बन्ध था अब उसका शायद पाँच प्रतिशत भी शेष नहीं रहा। अब सोने और चाँदी की मालियत में एक और बीस का अनुपात भी नहीं रहा। इसलिए चाँदी को अस्ल न माना जाए, बल्कि सोने को अस्ल माना जाए। उस ज़माने में पाकिस्तान इस्लामी वैचारिक परिषद के जो सदस्य थे उनकी अधिकांश संख्या ने इससे सहमति व्यक्त की थी। लेकिन उस ज़माने में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने इससे सहमति व्यक्त नहीं की और उन्होंने चाँदी को ही ‘दियत’ का एक मात्र आधार क़रार दिया। बहरहाल शरीअत में तीनों विकल्पों की गुंजाइश मौजूद है। इस समय पाकिस्तान में ‘दियत’ की मालियत का निर्धारण चाँदी के आधार पर होता है। और क़ानून मंत्रालय हर वर्ष नोटिफ़ाई करता है कि इस वर्ष चाँदी की क़ीमत इतनी है। उसके हिसाब से चाँदी की क़ीमत देनी पड़ती है जो आजकल की मालियत के हिसाब से लगभग तीन साढ़े तीन लाख रुपये बनती है। मेरे ख़याल में यह ‘दियत’ बहुत कम है। अगर ऊँट के हिसाब से ‘दियत’ अदा की जाए तो बहुत ज़्यादा बनेगी। सोने के हिसाब से देखा जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा बनेगी। सन् 1990 में जब यह हिसाब-किताब कर रहे थे तो उस समय चाँदी के हिसाब से कोई 75000 रुपये के क़रीब बनती थी और सोने के हिसाब से 12 लाख रुपये के क़रीब बनती थी। अगर उस समय सोने के हिसाब से बारह लाख रुपये ‘दियत’ तय कर दी जाती या आज सोने के हिसाब से तय कर दी जाए तो यह वास्तव में एक मज़बूत deterrent होगा। और अगर एक व्यक्ति एक गाँव में एक-बार ‘दियत’ अदा कर देगा तो आइन्दा पचास वर्षों के दौरान उस गाँव में कोई असावधानी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क़त्ले-ख़ता की ‘दियत’
क़त्ले-ख़ता की ‘दियत’ में एक बड़ा निराला-सा आदेश दिया गया है, जिसपर आजकल के लोगों को सन्तोष नहीं है, इसलिए वे अभी तक इसपर कार्यान्वयन करने पर तैयार नहीं हैं। इसपर पाकिस्तान में 1978 से बहस हो रही है। इसके समर्थक और विरोधी उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क और जवाबी तर्क दे रहे हैं। मुझे भी जब मौक़ा मिलता है तो अपने सुझाव पेश करता रहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में क़ानून बनानेवाले लोग अभी तक इसपर सन्तुष्ट नहीं हुए। शरीअत का कहना यह है कि जहाँ क़त्ले-ख़ता घटित होगा और वहाँ किसी व्यक्ति की ग़लती से किसी बेगुनाह इंसान की जान चली जाए तो मृतक के वारिसों को ‘दियत’ का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ तीन शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल यह हो सकती है कि आप कहें कि चूँकि मात्र ग़लती से जान चली गई है इसलिए आप सब्र करके बैठ जाएँ। अगर एक ग़रीब आदमी ट्रक के नीचे आकर मर गया तो उसको यह कहकर सन्तुष्ट कर दें कि बस अल्लाह की मर्ज़ी यही थी कि एक ग़रीब ड्राइवर के हाथों एक दूसरा ग़रीब आदमी मर गया। दूसरी सम्भावित शक्ल यह हो सकती है कि ट्रक चलानेवाले और आदमी मारनेवाले को जेल भेज दिया जाए। अब जेल क्यों भेज दिया जाए। उसने कोई इरादे से तो क़त्ल नहीं किया। उसको जेल भेजना ज़्यादती मालूम होती है। तीसरी शक्ल यह हो सकती है कि इस स्थिति में सरकारी ख़ज़ाने से ‘दियत’ अदा कर दी जाए। लेकिन यह सूरत भी बुराई से ख़ाली नहीं। अगर सरकारी ख़ज़ाने से ‘दियत’ अदा करनी शुरू कर दी जाए तो इंसानी जान इतनी सस्ती हो जाएगी कि जो जिसको मारना चाहेगा वह मारकर कह दिया करेगा कि क़त्ले-ख़ता हो गया है, सरकारी ख़ज़ाने से ‘दियत’ अदा कर दी जाए। लोग अपने किसी दुश्मन को ज़िन्दा नहीं छोड़ेंगे और कोई-न-कोई बहाना करके क़त्ले-ख़ता में दुश्मनों को मरवा दिया करेंगे, इसलिए कि कोई criminal liability नहीं होगी। अत: ये तीनों विकल्प स्वीकार्य नहीं। इन तीनों में ज़ुल्म पाया जाता है। शरीअत ने इन तीनों विकल्पों को अपनाया नहीं, बल्कि एक चौथे विकल्प को अपनाया। यह विकल्प ‘आक़िला’ का विकल्प है, जिसमें अपराधी की बिरादरी, क़बीला या हमपेशा लोग उसकी तरफ़ से क़िस्तों में ‘दियत’ अदा करते हैं।
शरीअत के इस ऑपशन के पीछे तत्वदर्शिता यह है कि आप अगर क़त्ले-ख़ता की सौ घटनाओं को जमा करें तो आपको पता चलेगा कि इन सौ में से कमो-बेश साठ-सत्तर घटनाएँ ऐसी होंगी जो क़त्ले-ख़ता करनेवाले व्यक्ति की ग़ैर-ज़िम्मेदारी या ढिलाई से घटित हुई होंगी। जिसने ट्रक रिवर्स किया, अगर वह सावधानी से काम लेता और पहले देख लेता कि कोई पीछे तो नहीं है, तो यह दुर्घटना घटित न होती। यह उसकी ज़िम्मेदारी थी। एक नॉर्मल सेंस और एक सामान्य बुद्धि और ज़िम्मेदारी के इंसान को यह देखना चाहिए कि उसके किसी कर्म या गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी का कोई नुक़्सान तो नहीं होगा। उसने चूँकि असावधानी बरती और थोड़ी-सी ग़लती भी की। इसलिए इस असावधानी को रोका जाना चाहिए। इसी तरह से जिसने इंसान को बत्तख़ समझकर देखे बिना गोली चला दी, उसको चाहिए था कि पहले जाकर देखता। वहाँ अगर इंसानों की मौजूदगी की सम्भावना थी, लोग शिकार के लिए आए हुए थे तो या तो उसकी निगाह इतनी मज़बूत होती कि नज़र आता कि वह जहाँ निशाना लगा रहा है वह कोई बत्तख़ नहीं, बल्कि इंसान है। अगर नज़र उतनी तेज़ नहीं थी तो चेक करना चाहिए था। थोड़ी ग़ैर-ज़िम्मेदारी यहाँ भी हुई। जहाँ भी कोई ग़ैर-ज़िम्मेदारी होगी, असावधानी वहाँ ज़रूर होगी। अब इसपर ग़ौर करें कि किन परिस्थितियों में इंसान असावधानी करता है। इंसान आम तौर से उन परिस्थितियों में असावधानी करता है जहाँ वह यह महसूस करे कि उसके पीछे कोई बड़ी ताक़त है। बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के बेटे careless होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े ज़मींदारों के बच्चे प्रसिद्ध लोगों की सन्तान, बड़े लोगों के कर्मचारी असावधान होते हैं। यह आम देखने में आता है, आप ख़ुद देख लें। अगर असावधानी की घटनाओं का जायज़ा लें तो नव्वे प्रतिशत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पीछे कोई बड़ी प्रभावशाली शक्ति या व्यक्तित्व होता है। किसी बड़ी राजनैतिक दल की ताक़त है और वे सोचते हैं कि हमें कौन पूछता है, हमारी पार्टी की हुकूमत है। अगर किसी की साइकिल को टक्कर लग गई या किसी का ठेला उलट गया तो क्या होता है। हमारी पजीरू की टक्कर से उसके फल ज़मीन पर गिर कर बिखर गए तो क्या हो गया। इस तरह असावधानीपूर्ण घटनाओं के पीछे यह रवैया होता है।
‘आक़िला’ की धारणा
इसलिए यह फ़ैसला अत्यन्त गहरे मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। शरीअत ने क़त्ले-ख़ता में ‘दियत’ का आदेश दिया है। लेकिन क़त्ले-ख़ता में ‘दियत’ वे लोग अदा करेंगे जो इस व्यक्ति के पृष्ठपोषक हैं और जिनके संरक्षण की वजह से इस आदमी ने इस असावधानी का प्रदर्शन किया है। उनपर सामूहिक तौर पर ‘दियत’ डाली जाएगी। वह इस तरह से सामूहिक तौर पर ‘दियत’ अदा करेंगे कि उनमें से किसी व्यक्ति पर अनुचित बोझ न पड़े। तीन वर्ष के अन्तराल में क़िस्तों से वह ‘दियत’ अदा करें और हर व्यक्ति उतना अदा करे जितना कि वह आसानी से कर सकता हो। इसमें शरीअत ने कोई हदबंदी नहीं की कि वार्षिक कितना लिया जाए और मासिक कितना लिया जाए। यह परिस्थितियों पर छोड़ दिया है। सिद्धान्त यह है कि ‘दियत’ की रक़म वे लोग सामूहिक रूप से भुगतान करें जो इस व्यक्ति को संरक्षण उपलब्ध करते हैं। जिनपर मान की वजह से उसमें ग़ैर-ज़िम्मेदारी या लापरवाही का एहसास पैदा हुआ। उनमें से किसी पर ग़ैर-ज़रूरी बोझ न डाला जाए। उनको एक ही समय में भुगतान पर मजबूर न किया जाए। तीन वर्ष में क़िस्तों में भुगतान करें। कौन कितनी क़िस्त दे, कौन लोग हों, इस मामले को शरीअत ने मौलिक निर्देश देने के बाद छोड़ दिया है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुबारक दौर के शुरू-शुरू में यह ‘दियत’ आदिवासी चुकाया करते थे। क़ातिल का क़बीला अदा करता था। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जब क़बाइली व्यवस्था कुछ प्रभावित हो गई और मदीना मुनव्वरा, कूफ़ा और बस्रा जैसे शहरों में विभिन्न क़बीले के लोग आकर आबाद हो गए तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने दीवान के आधार पर फ़ैसला किया कि एक सरकारी रजिस्टर में सिपाहियों के नाम लिखे हुए होते हैं तो वे एक यूनिट या दीवान का जो संग्रह होगा उन लोगों से ‘दियत’ वुसूल की जाएगी।
मैं निजी तौर पर यह समझता हूँ। मैंने इसपर लिखा भी है और लेख भी हैं कि इस दौर में यह व्यवस्था न केवल व्यावहारिक है, बल्कि इससे बहुत-सी बड़ी-बड़ी ख़राबियों को रोका जा सकता है। इस तरह सामूहिक ‘दियत’ अदा करनेवालों को ‘आक़िला’ कहते हैं। ‘आक़िला’ की यह व्यवस्था अत्यन्त उचित, अत्यन्त तत्वदर्शिता पर आधारित और न्यायपरक भी है। अगर ‘आक़िला’ की व्यवस्था हो तो इससे बहुत-सी समस्याओं और मुश्किलों से बचने में सहायता मिल सकती है। आपने देखा होगा कि नौजवान लड़के तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जाते हैं। पूछें तो पता चलता है कि अमुक बड़े आदमी का, आई जी साहब, सेक्रेटरी साहब या जनरल साहब का बेटा है। इसलिए गाड़ी भगाए लिए चलता है और उसमें दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। कोई पूछनेवाला नहीं। लेकिन अगर पुलिस के तमाम अधिकारी मिलकर आज एक आई जी के बेटे की ‘दियत’ अदा करें और तीन वर्ष तक उनकी तनख़्वाहों से कटौती होती रहेगी तो जब किसी पुलिस ऑफ़िसर का बच्चा गाड़ी तेज़ चलाएगा तो दस पुलिसवाले उसको रोककर मना करेंगे और कहेंगे कि भाई साहब अभी तक तो पहली दुर्घटना की ‘दियत’ का भुगतान पूरा नहीं हुआ। अगर किसी क़बीले के या इलाक़े के लोगों के हाथों कोई ऐसी घटना हो जाए और उस बिरादरी के लोग तीन वर्ष तक ‘दियत’ अदा करते रहें तो कल कोई थोड़ी-सी असावधानी भी करेगा तो बीस आदमी खड़े होकर कहेंगे कि भाई मैं अपनी कमाई से तेरे लिए मासिक इतना भुगतान कर रहा हूँ, तू फिर भी बाज़ नहीं आया। लोग उसको रोकेंगे और एक प्रेशर क़ायम होगा। इस प्रेशर के परिणामस्वरूप वह नैतिक वातावरण पैदा होगा जिसमें ‘तवासी बिलहक़्क़’ (हक़ और सही बातों की नसीहत करना) और ‘तवासी बिस-सब्र’ (सब्र की नसीहत) का वातावरण क़ायम होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था अगर बने और चले तो यह ठीक शरीअत के स्वभाव के अनुसार है। इसके बहुत लाभ होंगे।
हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने इसपर यह आपत्ति की कि इस दौर में बड़े-बड़े शहरों में ‘आक़िला’ की शनाख़्त (identification) नहीं हो सकती। इसकी शनाख़्त की भी हमने कोशिश की। मैंने ‘आक़िला’ की definition तैयार की। जस्टिस मुहम्मद हलीम, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान थे, उनको मैंने दिखाया कि यह परिभाषा देख लें कि व्यावहारिक और ठीक है कि नहीं। उन्होंने मंज़ूरी दे दी। पेशावर हाईकोर्ट के एक जज को दिखाया, उन्होंने भी सही क़रार दिया। दो सीनियर वकीलों को दिखाया कि इस ‘आक़िला’ की identification में कोई समस्या तो नहीं होगी। उन्होंने कहा, नहीं होगी। क़ानून मंत्रालय के कुछ लोगों ने कुछ मुश्किलों की निशानदेही की, वे मैंने दूर कर दीं। और मेरा ख़याल था कि हमने तमाम आपत्तियों के उत्तर दे दिए। लेकिन जब फ़ैसला करनेवालों ने फ़ैसला किया तो फिर क़ानून के ड्राफ़्ट से ‘आक़िला’ के सिद्धान्तों से सम्बन्धित धाराओं को निकाल दिया गया। बहरहाल एक-न-एक दिन सर्वोच्च अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। बहुत-से मामलों का एक समय निर्धारित है। इसका भी एक समय नियुक्त होगा। एक-न-एक दिन ये सब काम होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम और आप अपने ज़ेहन को साफ़ रखें। अपने सीमित ज्ञान और त्रुटिपूर्ण विचारों के आधार पर मामलों के अन्तिम फ़ैसले करने से गुरेज़ करें।
Recent posts
-
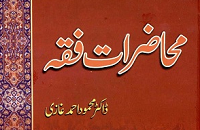
इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (लेक्चर #10)
23 March 2025 -
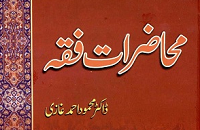
इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -
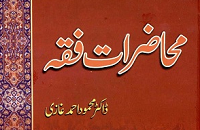
शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -
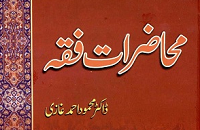
इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025 -
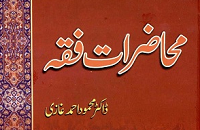
फ़िक़्ह का सम्पादन और फ़क़ीहों के तरीक़े (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 5)
26 February 2025 -
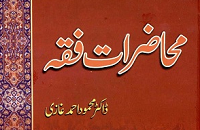
इल्मे-फ़िक़्ह के विभिन्न विषय (फ़िक़्हे इस्लामी : लेक्चर 4)
25 February 2025

