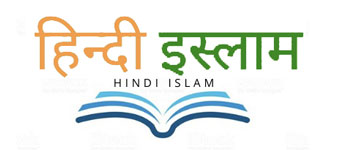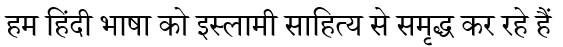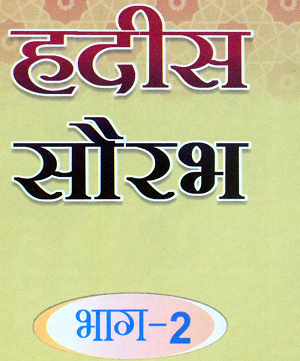
हदीस सौरभ भाग-2 (अनुवाद एवं व्याख्या सहित)
-
हदीस
- at 01 July 2024
हदीस सौरभ
(अनुवाद एवं व्याख्या सहित)
भाग-2
लेखक : मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ
प्रकाशक : मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स
बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
“दयावान कृपाशील परमेश्वर के नाम से"
दो शब्द
प्रस्तुत है, हदीस सौरभ भाग-2। इससे पूर्व इस पुस्तक का प्रथम भाग प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रथम भाग में इस्लाम की मौलिक धारणाओं और इबादतों से सम्बन्धित हदीसों को संगृहीत किया गया है और हदीस सौरभ भाग-2 में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नैतिक शिक्षाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे चीज़ें क्या हैं जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दृष्टि में अनैतिक हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का जीवन वास्तव में आदर्श जीवन है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हैसियत चरित्र-नायक की है। प्रस्तुत पुस्तक के अन्त में यह दिखाया गया है कि नैतिक दृष्टि से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्थान अत्यन्त उच्च है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है।
मनुष्य में नैतिक चेतना पाई जाती है। इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। यह नैतिक चेतना पदार्थ (Matter) की देन नहीं हो सकती। इसका स्रोत तो वही सत्ता हो सकती है जो जीवन्त और सामर्थ्यवान हो और साथ ही उसमें दानशीलता का अपार गुण भी विद्यमान हो। कांट, जो आधुनिक युग का सुप्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है, नैतिक चेतना को ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण स्वीकार करता है।
नैतिक चेतना वास्तव में चेतना का उच्चतम स्तर है। समस्त भलाइयों की आधारशिला नैतिक चेतना ही है। मनुष्य के नैतिक अस्तित्व के कारण ही ईश्वर ने उसको सम्बोधित किया है और इस सिलसिले में उसने मनुष्य का पूर्ण मार्गदर्शन किया है, जिससे ज्ञात होता है कि नैतिकता का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन से है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के विचार और व्यवहार दोनों ही से है। यह मानव-मन का मात्र एक भाव नहीं है, बल्कि यही समग्र जीवन है।
अल्लाह पर ईमान लाने और उसे अपना रब स्वीकार करने का स्पष्ट प्रभाव मनुष्य की नैतिकता पर पड़ता है। ईमान से एक सजीव एवं उत्कृष्ट नैतिकता का और उससे एक पवित्र एवं उत्कृष्ट जीवन का आविर्भाव होता है। नैतिकता सम्पूर्ण जीवन में क्रियान्वित दीख पड़ती है और जीवन का कोई क्षेत्र भी उससे रिक्त नहीं दिखता।
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि.), हिन्दी भाषा में इस्लामी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के शुभ कार्य में लगा हुआ है। इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आशा है कि इसे पसन्द किया जाएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी।
इस किताब का हिन्दी अनुवाद जनाब तारिक़ अहमद सिद्दीक़ी साहब ने किया है जिसे स्वयं इस किताब के लेखक मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ साहब ने शब्दशः देखा है। मौलाना के अलावा ट्रस्ट के अन्य साथी कौसर लईक़ साहब, ख़ालिद निज़ामी साहब और मुहम्मद शुऐब साहब ने भी इसे प्रूफ़ आदि की दृष्टि से सुधारा है। हम इन सभी के आभारी हैं। ख़ुदा का शुक्र है कि मुझे भी इस पुस्तक को पढ़ने और विषय आदि की दृष्टि से सुधारने का अवसर मिला।
हमारा प्रयास रहा है कि इस पुस्तक में प्रूफ़ आदि की कोई त्रुटि न रहे, फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें अवश्य सूचित करें, ताकि उसका सुधार किया जा सके। इसके लिए हम आभारी होंगे।
नसीम ग़ाज़ी फ़लाही
अध्यक्ष
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, दिल्ली
20-03-2010
बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
“दयावान कृपाशील परमेश्वर के नाम से"
अध्याय-1
नैतिकता
(1)
नैतिकता का महत्व और आवश्यकता
नैतिकता का महत्व
नैतिकता को मानव जीवन में जो महत्व प्राप्त है उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। इतिहास में किसी ऐसी सभ्यता का उदाहरण नहीं मिलता जिसमें सत्य और असत्य की सिरे से कोई कल्पना और धारणा ही न पाई जाती हो। जो लोग नियतिवाद (Determinism) के समर्थक हैं वे भी खुलकर इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनकी दृष्टि में झूठ और सच में या ईमानदारी और बेईमानी में कोई अन्तर नहीं है।
इससे कौन इनकार कर सकता है कि सच्चाई, शुभेच्छा और नियमबद्ध आचरण मानव के अपेक्षित गुण हैं। मानव की अन्तरात्मा के लिए यह कभी सम्भव नहीं हो सकता कि वह वचनबद्धता तुलना में छल-प्रपंच को और त्याग और आत्मोत्सर्ग के स्थान पर स्वार्थपरता को और प्रेम और बन्धुत्व की तुलना में ईर्ष्या-द्वेष और अत्याचार को श्रेष्ठतर समझने लगे।
मानव से किसी विशेष प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा रखने का अर्थ यह है कि हम मानव के संकल्प-स्वातंत्र्य में विश्वास करते हैं। इसलिए कि जहाँ कोई संकल्प और चुनाव की आज़ादी न पाई जाती हो वहाँ किसी चरित्र और नैतिकता का सवाल ही नहीं उठता। यह एक तथ्य है कि नैतिकता का सम्बन्ध मानव के संकल्प और चुनाव की आज़ादी से है। मानव को दुनिया में संकल्प और चुनाव की स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिए उसका एक नैतिक अस्तित्व है। यही चीज़ है जो उसे अन्य जीवों की तुलना में विशिष्टता प्रदान करती है।
मानवीय चरित्र और उसके कर्म की कोई भौतिक व्याख्या सम्भव नहीं। चेतना को जड़ की उत्पत्ति समझना सत्य नहीं। जड़ पदार्थों का अध्ययन एक भौतिक शोध हो सकता है किन्तु भौतिक साधनों के द्वारा चेतना की व्याख्या किसी प्रकार नहीं की जा सकती। मैक्स प्लैंक (Max Plank) ने कहा है :
“कोई व्यक्ति, चाहे कितना ही अक़्लमन्द क्यों न हो, मात्र कारण-कार्य नियम के द्वारा अपने सचेतन कर्मों के निर्णायक प्रेरकों के सम्बन्ध में कभी भी सही परिणाम पर नहीं पहुँच सकता। इसके लिए किसी अन्य नियम अर्थात नैतिक नियमों की आवश्यकता है।" (The Universe in the Light of Modern Physics)
मानव को संकल्पवान अस्तित्व समझने के लिए आवश्यक है कि मानव की स्थायी और स्वतन्त्र हैसियत को स्वीकार किया जाए। क्योंकि इसके बिना उसे नैतिक और चारित्रिक गुणों से सम्पन्न मानने का कोई औचित्य शेष नहीं रहता।
नैतिकता और चरित्र के लिए संकल्प और चुनाव की स्वतन्त्रता के अतिरिक्त ऐसे वास्तविक, स्थायी और निरपेक्ष (Real, Permanent and (Absolute) जीवन-मूल्यों की भी आवश्यकता है जो नैतिक नियमों का आधार बन सकें। जिनका मूल्य और महत्व सापेक्ष और अस्थायी न हो, बल्कि उनका मूल्य स्थायी और अपना स्वयं का हो, जिनकी सुरक्षा के लिए आदमी अपना सब कुछ क़ुरबान कर सके।
नैतिकता और परम अभीष्ट सत्ता
इसके अतिरिक्त मानव जीवन में किसी उच्च नैतिक व्यवस्था की कल्पना उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक मानव का कोई ऐसा अभीष्ट न हो जो परम और अन्तिम हो, जिसकी ओर बढ़ने में हम अपने तमाम प्रयासों को लगाकर शान्ति पा सकें और जिस तक पहुँचने पर हमारी अपनी पूर्णता (Perfection) भी निर्भर करती हो। जीवन का कोई उच्च अभीष्ट और अभिप्राय ही आदमी को हर प्रकार की पथभ्रष्टता और बिखराव से बचाकर प्राकृतिक और स्वाभाविक मार्ग पर लगा सकता है। इसी की प्राप्ति का प्रयास मानव की सच्ची सफलता और उसके व्यक्तित्व की पूर्णता की ज़मानत हो सकता है। इसके बिना हमारे जीवन में भी और विशेष रूप से हमारे आन्तरिक जीवन में सन्तुलन पैदा नहीं हो सकता। ऑस्पन्सकी (Ospunsky) ने लिखा है—
“मानव जब तक अपने अन्तर्विरोधों में ऐक्य न उत्पन्न कर ले, उसे अपने आप को मैं कहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कि इसके बिना उसका अपना कोई संकल्प ही नहीं है। जो व्यक्ति यह ऐक्य प्राप्त किए बिना अपने आप को संकल्पवान समझता है तो यह उसकी भूल (Error) है। संकल्प परिणाम होता है इच्छाओं का। जिस व्यक्ति की इच्छाओं में ही स्थायित्व न हो उसकी हैसियत मात्र अपनी भावनाओं और बाह्य प्रभावों के खिलौने की होगी। उसे ख़बर नहीं हो सकती कि दूसरी ही साँस में वह क्या कह देगा और क्या कर गुज़रेगा। उसके जीवन के प्रत्येक क्षण पर आकस्मिकताओं (Chances) का परदा पड़ा होगा।" (The New Model of Universe)
नैतिकता और सत्यज्ञान
जीवन में आन्तरिक समायोजन का बड़ा महत्व है। आन्तरिक समायोजन के बिना समाज में भी किसी समायोजन और ऐक्य की आशा नहीं की जा सकती। रही समस्या नैतिक मूल्यों (Moral Values) की उपलब्धि की तो सत्यज्ञान के बिना यह स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता। राशडल (Rashdall) का यह विचार सत्यानुकूल है—
“यह सम्भव नहीं कि सत्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण नैतिकता की आधारभूत समस्याओं को प्रभावित न करे या हमारे नैतिक दृष्टिकोण से सत्य की हमारी अवधारणा प्रभावित न होती हो।”
सत्य की उपेक्षा करके किसी उच्च और दृढ़ नैतिक व्यवस्था की उपलब्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थायी और निरपेक्ष नैतिक मूल्यों के लिए अनिवार्य है कि जीवन का अपना कोई वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य हो, इस जगत् को किसी महान उद्देश्य के तहत अस्तित्व में लाया गया हो और जगत् की समस्त वस्तुएँ उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधनमात्र हों।
नैतिकता और जीवन की निरन्तरता
फिर इससे आगे बढ़कर किसी उच्च नैतिक व्यवस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि मानव अपने जीवन की निरन्तरता पर विश्वास रखता हो। क्योंकि अगर हमारा जीवन चिरस्थायी नहीं तो चिरस्थायी मूल्यों से हमारा सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि अगर लोगों का उद्देश्य केवल निकटस्थ हितों की प्राप्ति हो तो कभी भी उनके चरित्र में सन्तुलन पैदा नहीं हो सकता और न ऐसे लोगों द्वारा निर्मित समाज सुदृढ़ और मज़बूत हो सकता है।
मैकेनजी (Mackenji) ने नैतिक समस्याओं पर विचार करते हुए लिखा है—
“जब हम कहते हैं कि नैतिकता के अध्ययन का सम्बन्ध ऐसे मानव चरित्र से है जो सत्य और मंगल हो, तो इससे हमारा अभिप्राय यह है कि उसका सम्बन्ध इस दृष्टिकोण से होता है कि हमारा व्यवहार (Conduct) किसी ऐसे अन्तिम लक्ष्य या आदर्श के लिए लाभप्रद होता है जो हमारे समक्ष हो और उसका सम्बन्ध उन क़ानूनों और सिद्धान्तों से होता है जिनके मार्गदर्शन में हमारा चरित्र उस अभीष्ट या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा अपनाता है। यूँ तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम कार्य करते हैं, जैसे मकान बनाना, पुस्तक लेखन आदि, लेकिन नैतिकता में चरित्र का अध्ययन उसके समग्र रूप में (As a whole) ही अपेक्षित है। यह किसी विशिष्ट प्रकार के चरित्र का अध्ययन कदापि नहीं है। यह विभिन्न उद्देश्यों में से किसी एक से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता जो उसके समक्ष हो, बल्कि उसका सम्बन्ध उस बड़े और अन्तिम लक्ष्य से है जो हमारे पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन सिद्ध होता है। उस अन्तिम लक्ष्य को सामान्यतः 'परम शिव (Absolute Good)' कहा जाता है।" (A Manual of Ethics p.2)
दुनिया में सर्वाधिक आदरणीय और मूल्यवान वस्तु वह है जिसे यूनान के लोगों ने नाउस (Nous) या नोएटिक नाउस (Noetic Nous) कहा है। जिसको अरबी भाषा में नफ़्स या "नफ़्से-नातिक़ा" कहते हैं। इसी को भारत में आत्मा कहा गया है। आत्मा का पदार्थ से अलग अपना स्वतन्त्र स्थायी अस्तित्व है और कई पहलुओं से जगत् में उसे उच्चता प्राप्त है। जगत् में केन्द्रीय महत्व आत्मा का है। जगत् के सम्पूर्ण सौन्दर्य और आकर्षण की चेतना आत्मा के द्वारा होती है। इसी के कारण जगत् में अर्थवत्ता उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण जगत् का मूल और सार-तत्व आत्मा ही है। जगत् में जो वस्तुएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं वे आत्मा की सम्भावनाओं के सिवा और कुछ नहीं। आत्मा ही वह दीपक है जिसका प्रकाश चतुर्दिक फैला हुआ है। जब वास्तविक परिस्थिति यह है तो स्पष्ट है कि जगत् की कोई भी वस्तु मानव आत्मा की अभीष्ट नहीं हो सकती। आत्मा का अभीष्ट वही होगा जो उससे उच्चतर और महत्तर हो। इसलिए अनिवार्यतः मानवीय आत्मा का अभीष्ट और अन्तिम लक्ष्य एक परम आत्मा (Supreme and Absolute Personality) ही हो सकती है। हम यह स्वीकार कर सकते थे कि आत्मा प्रत्येक दृष्टि से स्वयं साध्य और अभीष्ट है लेकिन इसमें कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनका हल सम्भव नहीं। उदाहरणस्वरूप अपने समस्त गुणों और चमत्कारों के बावजूद आत्मा स्वयंभू नहीं, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई उसका स्रष्टा न हो। ऐसा अगर होता तो वह अपने आप में पूर्ण (Perfect in his Personality) होती। उसे स्वयं का पूरा ज्ञान होता, उसके लिए पथभ्रष्ट होने की संभावना ही न होती और उसके पूर्णता को प्राप्त करने का सिरे से कोई प्रश्न ही न उठता।
अगर आत्मा के अभीष्ट लक्ष्य को हम व्यक्तित्वहीन मानें तो इस रूप में वह मानवीय आत्मा की अपेक्षा निम्नतर कोटि की होगी और उसे कोई भी आत्मा का अभीष्ट नहीं मान सकता। इसलिए अनिवार्यतः अपना लक्ष्य और अभीष्ट कोई परम सत्ता (Absolute Personality) ही हो सकती है। और यह वही सत्ता है जिसको दुनिया ईश्वर, अल्लाह या God आदि नामों से जानती और पहचानती है। ईश्वर ही वास्तव में सभी सत्यों का स्रोत और हमारे अस्तित्व का वास्तविक केन्द्रबिन्दु है। सारांश यह कि एक श्रेष्ठतम नैतिक आदर्श की कल्पना परम सत्ता के बिना सम्भव नहीं और न पारलौकिक जीवन पर ईमान लाए बिना जीवन की निरन्तरता की गुत्थी सुलझती है जिससे नैतिक मूल्यों की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
नैतिकता, भौतिकवाद और वैश्विक अर्थवत्तापूर्ण नियम
मानव के लिए किसी ऐसी नैतिक व्यवस्था की अवधारणा, जिसका आधार भौतिकवाद के बजाय वैश्विक अर्थवत्तापूर्ण नियमों पर हो, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिससे हमारा जीवन कोई सामंजस्य न रखता हो। हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने हर सांसारिक मामले में कोई न कोई अर्थवत्तापूर्ण दृष्टिकोण रखने पर मजबूर है। इनसान अचेतन रूप में केवल यांत्रिक रूप से कोई कार्य नहीं करता। उसके प्रत्येक कार्य के पीछे उसका ज्ञान और संकल्प कार्यरत होता है। परिणामदर्शिता उसका स्वभाव है। विशुद्ध भौतिकवाद के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि कोई व्यक्ति नैतिक नियमों के अनुसार कर्म क्यों करे? अपने निकटतम हित को छोड़कर दूसरों के काम क्यों आए? कमज़ोरों और पीड़ितों के साथ हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों करें? इसमें सन्देह नहीं कि भौतिकवाद के झंडावाहकों में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी हैं। दरिद्रों, मुहताजों और मज़लूमों के समर्थन में वे सक्रिय रहे हैं, लेकिन उनकी यह कार्यशैली उनके मौलिक सिद्धान्तों से मेल नहीं खाती। निश्चय ही यह भौतिकता का नहीं भौतिकता से परे किसी और चीज़ का प्रभाव था जो उनके मन के किसी कोने में छिपा रहा है।
मौलिक आवश्यकता
नैतिक मूल्यों की प्राप्ति मानव की मौलिक आवश्यकता है। नैतिकता ही वह मूल्यवान तत्त्व है जिसके द्वारा आध्यात्मिक, भौतिक और सौन्दर्यात्मक (Aesthetic) मूल्यों में समायोजन और समरसता उत्पन्न की जा सकती है। इसी के द्वारा समाज में पाए जानेवाले अन्तर्विरोध पारस्परिक सामंजस्य में परिवर्तित हो सकते हैं। नैतिकता ही वह शक्ति है जिससे मानव जीवन उस सत्य के साथ जीवन का तारतम्य स्थापित करता है जो परिवर्तनों से परे है। सत्य के साथ यही समन्वय और समरसता है जिसको विचारकों ने वास्तविक स्वतन्त्रता और सत्य की उपलब्धि से अभिव्यंजित किया है।
भौतिकता या नैतिकता
भौतिकवाद के पक्षधर पदार्थ ही को सब कुछ समझते हैं। उनकी दृष्टि में यहाँ जो कुछ भी है वह मात्र भौतिक पदार्थों का चमत्कार है। उदाहरणस्वरूप कतिपय भौतिकवादियों का मत यह है कि अर्थव्यवस्था की संरचना ही में मानव जीवन का सम्पूर्ण रहस्य निहित है। धर्म और नैतिकता, सभ्यता और संस्कृति सब आर्थिक परिस्थितियों की पैदावार हैं। वस्तुतः यथार्थ का यह अत्यन्त सतही अध्ययन है। मार्क्स और उसके अनुयायी कम से कम मनोविज्ञान और मानवशास्त्र ही से परिचित होते तो मनोविज्ञान उन्हें बताता कि उत्पादन के साधन मानव मस्तिष्क की क्रियाओं और प्रविधियों की व्याख्या में सर्वथा असफल हैं। मानव-मन उत्पादन के साधनों को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है और उनपर प्रभाव डालता है। मानव विज्ञान उन्हें इस बात से परिचित कराता कि मानवीय आत्मा मात्र भ्रम या भ्रम की निर्मिति नहीं है, बल्कि मानव संस्कृति के उद्भव और विकास में वस्तुतः आत्मा ही अपने को व्यक्त करती है। भौतिक साधनों को वही काम में लाती है और उनसे काम लेकर विभिन्न शैलियों की रचना करती है। विभिन्न शैलियों में उसी की अभिव्यक्ति होती है।
स्वयं यह जगत् मात्र उपादेयता (Utility), अर्थात जिससे हमारे भौतिक हित जुड़े होते हैं, को ही व्यक्त नहीं करता। इस जगत् में दूसरे अन्य ध्यान देने योग्य संकेत भी पाए जाते हैं जो उपयोगिता और उपादेयता से श्रेष्ठतर हैं, जिनकी उपेक्षा करते हुए जगत् की जो भी व्याख्या की जाएगी दोषपूर्ण और ग़लत होगी। जगत अर्थमय है और जीवन की अपनी अर्थवत्ता है जिसे जानने में भौतिकवाद नितान्त असमर्थ है। जगत् में स्पष्टतया किसी उच्च और श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान और संकल्प कार्यरत प्रतीत होता है। जगत् में किसी के संकल्प और ज्ञान के कार्यरत होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि यहाँ समस्त क्रियाशीलता नैतिकता की है। ज्ञान और संकल्प की अभिव्यक्ति सदैव नैतिकता के साथ होती है। उदाहरणार्थ आप देखेंगे कि मानव की आवश्यकताओं और जगत् द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली वस्तुओं में अत्यन्त गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। शरीर को बनाए रखने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन सबको मानव अपने आस-पास जगत् में विद्यमान पाता है। ये बहती नदियाँ, जलस्रोत और मैदान, ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष और जानवर, ये फल-फूल और खेतियाँ मानव की प्राकृतिक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के उत्तर हैं। इन्हें स्रष्टा की अनुकम्पा के सिवा किसी और चीज़ से अभिव्यंजित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें, जिन्हें हम अपने चतुर्दिक देखते हैं, वास्तव में ईश्वरीय स्वभाव ही के जीवन्त प्रतीक हैं। यह इस बात का खुला प्रमाण है कि जगत् में वास्तव में भौतिकता नहीं बल्कि नैतिकता कार्यरत है।
नैतिक कार्यशीलता की इससे भी ज़्यादा साफ़ और स्पष्ट तस्वीरें मौजूद हैं लेकिन मानव उनकी ओर बहुत कम ध्यान देता है। आप जानते हैं कि बच्चे के पालन-पोषण में वास्तविक भूमिका माता-पिता या सगे-सम्बन्धियों के उस वात्सल्य और प्रेम की होती है जो उन्हें बच्चे से होता है। यह नैतिकता का चमत्कार है न कि विशुद्ध भौतिकता का! इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर अगर हमें सौन्दर्यबोध प्रदान किया गया है तो दूसरी ओर जगत् की प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य पाया जाता है। इसे मात्र भौतिक तत्वों की करामात ठहराना और इसी पर होकर रहना बौद्धिक और वैचारिक आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मार्क्स और दूसरे भौतिकवादी इस तथ्य को समझने में असमर्थ हैं कि जीवन को जड़ और भौतिक पदार्थों पर श्रेष्ठता प्राप्त है। एक श्रेष्ठतर वस्तु अपने से निम्नतर के अधीन क्योंकर हो सकती है। जीवन चेतना और अनुभूतियों से भरी एक आबाद दुनिया है जिसका स्रोत कोई चैतन्य और परम सत्ता ही हो सकती है, और केवल वही सत्ता जीवन का अभीष्ट और अभिप्राय हो सकती है। ईश्वर को अपने जीवन से विलग करके न केवल यह कि मानव ईश्वर के अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर देता है बल्कि उसकी यह नीति स्वयं उसके अपने विरुद्ध भी है, क्योंकि इस प्रकार वह अपनी हैसियत को गिरा देता है। इस बात को एक मिसाल के द्वारा समझा जा सकता है। हमारे शरीर के समस्त अवयव हाथ, पैर आदि देखने में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं किन्तु सत्य यह है कि इनकी हैसियत जो कुछ है वह हमारे व्यक्तित्व के सापेक्ष है। अगर हमारे हाथ और पैर हमारे व्यक्तित्व के अधीन न हों तो उनका अस्तित्व निरर्थक होकर रह जाए। शारीरिक व्यवस्था में केन्द्रीय महत्व हमारे व्यक्तित्व को प्राप्त है। इसलिए हमारे समस्त अवयव अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए प्रति क्षण हम पर निर्भर करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी वास्तविक हैसियत का निर्धारण ईश्वर की ओर से होता है। इस सम्बन्ध और सम्पर्क के बिना हमारी हालत एक ऐसे हाथ-पैर की रह जाती है जिसको शरीर से काट कर फेंक दिया गया हो। ऐसे कटे हुए हाथ-पैर और मिट्टी के ढेर में कोई मौलिक अन्तर शेष नहीं रहता। मानव यह तो समझता है कि हाथ या पैर का शरीर से कटकर अलग होना उसके लिए घातक है किन्तु अपनी दृष्टिहीनता के कारण वह उस घातक परिस्थिति को महसूस करने में सामान्यतः असमर्थ रहता है जिसमें वह ईश्वर से अलग होकर जा पड़ता है।
नैतिकता बोझ नहीं
नैतिकता मानव के लिए कोई अप्रिय बोझ कदापि नहीं है। रंग और सुगन्ध फूलों पर बोझ नहीं। परिन्दों के पंख परिन्दों के लिए कभी भार नहीं होते, बल्कि ये पर उनकी शोभा भी हैं और उड़ान में उनके सहायक भी। यही हाल फूलों के रंग और गन्ध और आँखों की पलकों का भी है। मानव जीवन में भी वास्तविक सौन्दर्य नैतिकता ही से उत्पन्न होता है। नैतिकता से वंचित हो जाने के बाद मानव के पास कोई मूल्यवान वस्तु शेष नहीं रहती। नैतिक अपेक्षाएँ हमारी प्रकृति और स्वभाव को ही दर्शाती हैं।
नैतिकता वास्तव में एक वैश्विक और व्यापक नियम का नाम है। वही हमारे आन्तरिक जीवन का भी नियम है। नैतिकता ही है जिसके द्वारा मानव के आन्तरिक जीवन में सन्तुलन और उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य और एकात्मता उत्पन्न हो सकती है। यही वह वैश्विक नियम है जिसे हम जगत् की व्यवस्था में भी देखते हैं। जगत् की समस्त वस्तुएँ एक सही और स्वाभाविक नियम के अधीन हैं जिसके पीछे ईश्वर का संकल्प क्रियाशील है। इसे स्वीकार करने पर आज बड़े-बड़े चिन्तक अपने को विवश पाते हैं। उन्हें यह मानना पड़ा है कि यह जगत् किसी मशीन के बजाय मन से अधिक सादृश्यता रखता है।
इसमें सन्देह नहीं कि भौतिक जीवन दर्शन उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में अपने यौवन पर था। किन्तु बीसवीं शताब्दी में स्वयं यूरोप के कितने ही विचारकों और वैज्ञानिकों को नए अनुसन्धानों और शोधकार्यों के पश्चात अपनी धारणा को बदलना पड़ा है। जे. एस. हाल्डेन ने लिखा है कि जीवन की समस्या को भौतिक और रासायनिक समस्या समझना ग़लत है। जीवन और मानव व्यक्तित्व (Personality) का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि विश्व की मात्र भौतिक व्याख्या सम्भव नहीं। (Prof. J.S. Haldane in "The Philosophical Basis of Biology")
विज्ञान ने अब हमें ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहाँ बड़े-बड़े वैज्ञानिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि विश्व में जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु (Thing) सिरे से है ही नहीं, बल्कि केवल कार्य है या घटनाओं (Events) का भवन है (Quoted by Iqbal in his Lectures)। इससे इस बात को अतिरिक्त बल मिलता है कि यह जगत् अन्धे बहरे भौतिक पदार्थ की संरचना नहीं बल्कि इसका अस्तित्व स्रोत कोई मन और संकल्प है। दूसरे शब्दों में जगत् ईश्वरीय रचनाकर्म की अभिव्यक्ति है। मानव का दायित्व है कि वह अपने संकल्प और कर्म-स्वातन्त्र्य की दुनिया में अपने प्रभु का आज्ञापालन करें। क़ुरआन में कहा गया है :
“निश्चय ही मेरा प्रभु सीधे रास्ते पर है।” (11:56)
मतलब यह है कि ईश्वर का कोई कार्य न्याय, तत्त्वदर्शिता और सत्य के विरुद्ध नहीं हो सकता। उसने सत्य और शिवम् (Good) के अन्तर्गत जगत् की रचना की है। हमें संकल्प और कर्म-स्वातन्त्र्य प्रदान करने से भी जो चीज़ अभीष्ट है वह सत्य और शुभ के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। मानव का कल्याण और उसकी सफलता उसके अन्तःकरण की शुद्धि पर निर्भर करती है। ज़ाहिर (बाह्य) और बातिन (अन्तर) को “ख़ल्क़" (Creation) और "ख़ुल्क़" (शील) से अभिव्यंजित किया जाता है। कहते हैं “फ़ुलानुन हुस्नुल ख़ुल्क़ि वल-ख़ल्क़” अर्थात “अमुक का अन्तर भी अच्छा है और बाह्य भी।” बाह्य को यदि हम आँख से देखते हैं तो अन्तर या आत्मा का बोध अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। बाह्य हो या अन्तर हरेक का अपना एक विशिष्ट रूप और आकार होता है। यह रूप और आकार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ख़ुल्क़ (शील) या मन का सुदृढ़ रूप ही है जिससे कर्मों का संचालन होता है। अगर हमसे अच्छे कर्म होते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि हमारा अन्तर्मन अच्छा है। इसी को सुशीलता से अभिव्यंजित करते हैं। मनुष्य के स्वभाव, प्रवृत्तियों और अभिरुचियों से उसके आन्तरिक रूपाकार का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। किसी की प्रवृत्ति और अभिरुचि को उसके चरित्र और व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। रस्किन (Ruskin) ने ग़लत नहीं कहा है कि अभिरुचि वास्तव में नैतिकता का कोई अंग या शाखा नहीं, बल्कि स्वयं अभिरुचि ही नैतिकता है। किसी को जाँचने के लिए पहला और अन्तिम सवाल जो उससे कर सकते हैं वह यही है कि उसे क्या पसन्द है? आदमी की पसन्द और नापसन्द से यह भेद खुल जाता है कि स्वयं वह आदमी क्या है।
नैतिकता के अध्ययन में सत्य, सुन्दर और शिव (Truth, Beauty and Goodness) को मौलिक महत्व दिया जाता है। इनका सम्बन्ध वास्तव में हमारे ज्ञान, अनुभव और कर्म से है। अगर आदमी सत्य के अनुसन्धान में असफल रहा तो वास्तव में वह सत्यज्ञान (True Knowledge) से वंचित है। उसका जीवन अगर एक सौन्दर्यानुभव में न ढल सका तो उसके एहसास (Feeling) की दुनिया वीरान ही रही। इसी प्रकार अगर वह 'शिवम्' को समझने में सफल न हो सका तो व्यावहारिक रूप से वह सर्वथा घाटे में रहा।
मानव का यह स्वभाव है कि वह जानना चाहता है कि सत्य और यथार्थ (Reality) क्या है? वह उन वस्तुओं को महत्व देता है जिनमें सौन्दर्य और गुणवत्ता हो। इसी प्रकार वह उस कर्म को अपनाना चाहता है जिसमें शिवम् निहित हो। साधारण अध्ययन में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन ही नैतिकता के अन्तर्गत किया जाता है। सत्य की उपलब्धि को दर्शन का विषय निश्चित किया गया है और सौन्दर्य तथा गुणवत्ता को सौन्दर्यशास्त्र (Aesthetics) के तहत रखा गया है। लेकिन जीवन के इन तीनों मूल्यों में इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ सत्कर्म को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। जो कर्म ज्ञान के अनुसार न हो वह पथभ्रष्टता है। सुक़रात ने कहा है :
“Virtue is a kind of knowledge.", “सत्कर्म ज्ञान ही का एक प्रकार है।"
सुक़रात का अभिप्राय यह है कि नैतिक दायित्वों के परिणाम अगर हम पर पूर्णरूपेण स्पष्ट हों तो अनिवार्यतः हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अनुचित नीति स्वयं अपने विरुद्ध एक अनुचित प्रयास है। अपने विरुद्ध कोई क़दम उठाकर कोई अपनी सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह कैसे कर सकता है।
नैतिकता और सौन्दर्य
नैतिकता से सौन्दर्यबोध को भी अलग नहीं कर सकते। अरस्तू (Aristotle) के दृष्टिकोण के अनुसार नैतिक जीवन स्वयं उसके अपने सौन्दर्य के कारण ही स्वीकार्य होता है :
Only Beauty is good. “सौन्दर्य ही शुभ है।”
सौन्दर्य का सम्बन्ध मात्र शरीर से ही नहीं है। नैतिक दृष्टि से भी कुछ चीज़ें सुन्दर (Morally Excellent) होती हैं। कांट (Kant) के शब्दों में वे हीरे की तरह स्वयं अपनी रौशनी से चमक रही होती हैं। वे उस वस्तु की तरह होती हैं जिसका मूल्य स्वयं उसके अपने अस्तित्व से स्थापित होता है।
नैतिकता और आनन्द
आनन्द (Pleasure) का भी नैतिकता से गहरा रिश्ता होता है। सही कार्यशैली से सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह प्रसन्नता मात्र आध्यात्मिक नहीं होती बल्कि बौद्धिक और हार्दिक होती है और साथ ही साथ सौन्दर्यबोध से भी इसका सम्बन्ध होता है। इसी लिए कहा गया है :
"Virtue is its own reward and vice is its own punishment."
“सत्कर्म अपना प्रतिदान स्वयं है और अपकर्म अपना दंड स्वयं है।"
नैतिकता और मनुष्य की पूर्णता
नैतिकता ही के द्वारा मनुष्य की पूर्णता सम्भव है। पूर्णत्व की उपलब्धि नैतिकता के बिना असम्भव है। ये और इस प्रकार के विचार जिन्हें विभिन्न विचारकों ने प्रस्तुत किए हैं, इनके द्वारा वास्तव में जीवन ही के विभिन्न पहलुओं और मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। नैतिकता के द्वारा जीवन का निर्माण होता है। नैतिकता जीवन को एक स्वरूप (Form) देती है। नैतिक मूल्यों का आदर जीवन के समस्त क्षेत्रों में अपेक्षित है।
नैतिकता में दार्शनिकों ने अपना प्रमुख दायित्व यह समझा है कि वे जीवन के परम लक्ष्य की खोज करें। प्लेटो और अरस्तू से लेकर स्पीनोज़ा, कांट, हीगल और ग्रीन तक सभी ने इस सम्बन्ध में अपने दायित्व के निर्वाह का प्रयास किया है। परम लक्ष्य के निर्धारण के बाद मानव का दायित्व स्वतः निर्धारित हो जाता है और इसकी अनिवार्यता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। इसी परम लक्ष्य के सन्दर्भ में मानव का पूरा जीवन अपना एक स्वरूप और आकार ग्रहण कर लेता है। चिन्तकों को उनके प्रयास ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वे यह मानने पर बाध्य हुए हैं कि जीवन के परम लक्ष्य (Ultimate Goal) का मानव के वर्तमान जीवन से इतना निकट का सम्बन्ध है कि वर्तमान जीवन और अस्तित्व को उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। जीवन उसी में प्रविष्ट और सम्मिलित है। नीतिशास्त्र के दार्शनिकों का काम केवल यह है कि वे इस तथ्य को इस सीमा तक स्पष्ट और लोगों की दृष्टि में इतना उजागर कर दें कि साधारण मानवीय चेतना भी इसे ग्रहण कर सके।
जहाँ तक विधि-विधान या क़ानून की बात है तो इस विषय में यह स्वीकार किया गया है कि नैतिकता और चरित्र का स्तर जब उच्च हो जाता है तो नैतिक नियम और सिद्धान्त मानव के लिए अजनबी नहीं रहते, बल्कि वे उसकी अपनी ही चेतना और अनुभूति का एक मूर्त रूप सिद्ध होते हैं। आदमी जिस चीज़ को अपने दिल की गहराई में पा रहा हो उसे धारण करने के लिए किसी बाह्य नियम और सिद्धान्त के दबाव की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे क़ानूनों और सिद्धान्तों के पालन का अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं कि आदमी स्वयं अपने साथ विश्वासघात न करे, वह स्वयं अपने लिए सच्चा हो।
"To Thine yourself Be true." "तुम अपने प्रति सच्चे बनो।"
नैतिक नियमों का विरोध स्वयं अपना विरोध है।
नैतिकता और मानव-समाज
मानव समाज से आदमी का गहरा सम्बन्ध होता है। वह अपने समाज का एक अंग होता है। विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। आदर्श व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति समाज के माध्यम से ही सम्भव है। इसलिए सामाजिक दायित्वों को मानवीय नैतिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। नैतिकता की सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण धारणा वही है जिसमें मानव के व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण का रहस्य निहित हो, जिससे कठिनाइयाँ सरल होती हों, उलझी हुई समस्याओं का अन्त हो जाता हो और हमारे मन-मस्तिष्क को शान्ति और आनन्द प्राप्त होता हो और जिसके द्वारा धरती अत्याचार और उपद्रव से मुक्त होती हो। ब्रिफ़ो (Briffaultt) का ध्यान इस ओर गया है। वह कहता है :
“आदर्श नैतिकता का कैसा ही भव्य भवन आप निर्मित कर लें, अगर वह असत्य को मिटा कर उसकी जगह सत्य को स्थापित करने में असमर्थ है तो वह निरर्थक चीज़ है। इस बाह्य भवन को नैतिकता का भवन नहीं कहा जा सकता।" (The Making of Humanity)
नैतिकता और धर्म
नैतिकता के महत्व और उसके विभिन्न पक्षों की चर्चा के बाद यह प्रश्न शेष रहता है कि मानव अपनी आचार संहिता और नैतिक व्यवस्था के लिए ऐसे स्पष्ट नियम और क़ानून कहाँ से प्राप्त करे जिनका पालन सबके लिए अनिवार्य हो, जिसके सत्य और श्रेष्ठ नैतिक व्यवस्था होने में किसी को सन्देह न हो सके। मानव-विज्ञानों में नियमबद्धता सुस्पष्ट नियमों के बिना सम्भव नहीं और न इसके बिना मानव विचार को विक्षिप्तता और बिखराव से बचाया जा सकता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर केवल धर्म के पास है। मानव विचार के सामने नैतिकता की प्राकृतिक माँगें तो उभर सकती हैं किन्तु धर्म के सहयोग के बिना परिपूर्ण और विश्वासयोग्य आचार संहिता देने में वह सर्वथा असमर्थ है। धर्म के अतिरिक्त दूसरे स्रोत चाहे वे मनोविज्ञान और अन्तःप्रवृत्तियाँ हों या अनुभव और अनुभूतियाँ, ये मूल स्रोत के केवल सहायक हो सकते हैं। इन्हें मूल स्रोत की हैसियत प्राप्त नहीं हो सकती। मात्र आंशिक सत्यों के ज्ञान से एक सर्वोच्च और सुदृढ़ नैतिक व्यवस्था की रचना कैसे सम्भव हो सकती है? एक निश्चित और अनिवार्यतः पालनयोग्य क़ानून की आवश्यकता का एहसास तो कांट (Kant) को भी हुआ है लेकिन वह इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या करने में असमर्थ दिखाई देता है।
नैतिकता के विषय में भलाई और बुराई या शुभ और अशुभ की सत्य धारणा का प्रश्न सामने आता है। किन्तु इसके हल करने में हमारा आनुभविक और अन्तःपरक ज्ञान अपर्याप्त सिद्ध होता है। बुद्धि इस सम्बन्ध में दूर तक हमारा साथ नहीं देती। नैतिकता की पृष्ठपोषक शक्ति और प्रेरणाओं के बारे में मानव विचार और चिन्तन ने जो चीज़ें प्रस्तावित की हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता, किन्तु धर्म का मार्गदर्शन न हो तो इन चीज़ों की हैसियत स्पष्ट नहीं होती और न इन्हें कोई सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है।
इस सम्बन्ध में जब हम इस्लाम का अध्ययन करते हैं, जो पूर्ण, प्रामाणिक और ईश्वर-प्रदत्त अन्तिम धर्म है, तो हमें उन सारे ही प्रश्नों का समुचित और सन्तोषजनक उत्तर मिल जाता है जो नैतिकता के अध्ययन में उभरकर हमारे सामने आते हैं। यहाँ हमें शुभ और अशुभ, नेक और बद, सही और ग़लत का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि ज्ञान का मूल स्रोत ईश्वरीय ग्रन्थ और उसका मार्गदर्शन है। ईश्वर ने जो नैतिक नियम प्रदान किए हैं उनके अनिवार्यतः पालन योग्य होने के लिए यही आधार पर्याप्त है कि वे ईश्वर की ओर से हैं। मानव के लिए जो परम लक्ष्य अपेक्षित है वह ईश्वर और उसकी प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ईश्वरीय सत्ता ही वह परम आत्मा और पूर्ण सत्ता है जिसे मानव का अन्तिम लक्ष्य और आश्रय कहा जा सकता है। अगर ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त किसी और चीज़ को हम जीवन और जगत् का अभिप्राय और प्रयोजन बताते हैं तो यह सत्य के प्रतिकूल और मानव पर अत्याचार होगा। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि मानव को दूसरी समस्त चीज़ों के मुक़ाबले में श्रेष्ठता और उच्चता प्राप्त है इसलिए उसका अभीष्ट कोई ऐसी चीज़ कदापि नहीं हो सकती जो व्यक्तित्व (Personality) के गुण से रहित हो। इसलिए अनिवार्यतः मानवीय अनुभवों और भावनाओं और उसके प्रयासों की दिशा ईश्वर ही की ओर होनी चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि तारे आसमान में देर तक चमकते हैं। चाँद हमारी अँधेरी रातों को रौशन कर देता है और सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त होती है, किन्तु हमारे अन्तर के लिए इनके पास कोई प्रकाश नहीं है और न हमारे दिल की गहराइयों में छिपी उमंगों के लिए इनके पास कोई गर्मी है। जगत् में जो भी है ईश्वर पर आश्रित और उसका मुहताज है। इसलिए उसके सिवा कोई नहीं जो हमारे जीवन और हमारे प्रयासों का केन्द्र बिन्दु बन सके।
मानव के लिए स्पष्ट कल्याण और भलाई की बात यह है कि वह उस परीक्षा में सफल हो जिससे वह दुनिया में दोचार है। जो नीति इस कल्याण को पाने में सहायक हो वही सही है और जो नीति इस कल्याण की प्राप्ति में सहायक न हो सके, बल्कि इस मार्ग में रुकावट बने, वह ग़लत है। ईश्वरीय मार्गदर्शन ही ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। ईश्वर का प्रेम, उसकी प्रसन्नता और रज़ामन्दी की चाह और उसकी अप्रसन्नता और नाराज़ी से बचने की चिन्ता, नैतिक व्यवहार की पाबन्दियों और अनैतिकता से बचने के लिए मूल प्रेरक है। ईशज्ञानी व्यक्तियों से मिलकर जो समाज और कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आता है, जिसका निर्माण ईश्वरप्रदत्त क़ानूनों की रौशनी में होता है, उसके अन्दर स्वयं ईश्वरीय नैतिक व्यवस्था की स्थापना की क्षमता होती है। फिर क़ानून के पालन के लिए दायित्वबोध भी पूर्णतया कार्यरत हो उठता है। और सत्य से प्रेम और असत्य से घृणा की भावना भी इस सम्बन्ध में एक प्रेरक है।
इस्लाम आंशिक सच्चाइयों का निषेध नहीं करता। वे सभी इस्लाम की नैतिक व्यवस्था में निहित दिखाई देती हैं। वे विच्छिन्न अंशों के रूप में या अपूर्ण दशा में मौजूद हों, इसके बजाय इस्लाम उनके लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराता है। इस्लाम पूर्णत्व प्राप्ति की इच्छा का, जिसे मानव विचार और चिन्तन की दृष्टि में एक नैतिक प्रेरक की हैसियत प्राप्त है, निषेध नहीं करता। बल्कि इस्लाम ने इसके महत्व की पुष्टि की है। क़ुरआन में है :
"तसबीह (महिमागान) करो अपने सर्वोच्च रब के नाम की जिसने पैदा किया, फिर ठीक-ठाक किया, जिसने निर्धारित किया, फिर मार्ग दिखाया, जिसने वनस्पति उगाई, उसे ख़ूब घना और हरा-भरा कर दिया।" (87:1-5)
मतलब यह है कि ईश्वर ने पैदा ही नहीं किया, उत्कृष्ट संरचना भी प्रदान की। फिर उसने उत्कृष्ट संरचना और प्राकृतिक सौन्दर्य ही नहीं प्रदान किया बल्कि परम लक्ष्य की ओर भी मार्गदर्शन किया। हम देखते हैं कि वह धरती में हरियाली और घास उगाता है और उसमें जो गुण छिपे होते हैं उन्हें उभारने और विकसित करने की व्यवस्था भी करता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि नन्हे-नन्हे अंकुर बढ़कर अत्यन्त घने, हरे-भरे और मनोरम वृक्ष हो जाते हैं। इस क़ानून से इन्सान का जीवन अलग नहीं है। ईश्वर ने इन्सान को केवल जीवन ही नहीं प्रदान किया बल्कि जीवन देकर जीवनोद्देश्य का भी ज्ञान दिया। वह मानव का उस मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है जिसपर चलकर वह अपने वास्तविक जीवनोद्देश्य को पा सकता है और अपने जीवन को पूर्णत्व तक ले जा सकता है। इस्लाम हमारे जीवन के सूक्ष्म और कोमल पक्षों का संरक्षक ही नहीं है बल्कि वह उन्हें उत्कृष्टता के चरम तक ले जाना चाहता है।
मानव का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वह अपने आप को पामाल कर दे और उसे पूर्णता से वंचित रखे। क़ुरआन में है :
"सफल हो गया वह जिसने उसे (अपने व्यक्तित्व को) विकसित किया। और असफल हुआ वह जिसने उसे दबा दिया।" (91:9-10)
पूर्णत्व वास्तव में अपने प्रभु की ओर बढ़ने ही पर निर्भर करता है। ईश्वर की उपेक्षा करके मनुष्य पस्ती में गिर जाता है और सफलता के ऊँचे दर्जे पर पहुँचने में असमर्थ रहता है। इस्लाम ने इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि मानव अपने पूर्णत्व के लिए सांसारिक परीक्षा के इस चरण में कौन-सी नीति अपनाए। इस सम्बन्ध में इस्लाम ने जो शिक्षा दी है उससे व्यक्ति ही नहीं, समाज, समुदाय और पूरी मानवता उन्नति की ओर बढ़ सकती है और लोग एक-दूसरे के पूर्णत्व में रुकावट होने के बजाय सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
यहाँ उस आनन्द (Pleasure) का भी निषेध नहीं किया गया है जिसका उल्लेख आचारशास्त्र के चिन्तकों के यहाँ मिलता है। लेकिन इसके साथ इसे भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ईश्वरीय प्रसन्नता की चाह और उसके लिए प्रयास और उसके दिए हुए क़ानून का पालन स्वयं सर्वाधिक आनन्द का विषय है। इस्लाम मन-मस्तिष्क और हृदय की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करता बल्कि वह मानव की समस्त भावनाओं और उसकी इच्छाओं का आदर करता है, शर्त यह है कि वे भावनाएँ और इच्छाएँ स्वाभाविक और ईश्वरीय आदेशों के अन्तर्गत हों। नैतिक दायित्वों के निर्वाह में जो प्रसन्नता होती है उसे तो इस्लाम ने दीन और ईमान का लक्षण कहा है। अतएव अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“जब तुम्हें अच्छे काम से प्रसन्नता हो और बुरे काम से दुख और क्षोभ हो तो तुम मोमिन हो।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
आनन्द चाहे मानसिक हो या आध्यात्मिक और सौन्दर्यबोध से सम्बन्धित, अगर उस आनन्द और धार्मिक मूल्यों के मध्य कोई टकराव न हो तो वह मान्य है। इस्लामी जीवन व्यवस्था में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति की प्रसन्नता और समाज और सम्पूर्ण मानवता के आनन्द के मध्य कोई विरोध और विसंगति न उत्पन्न हो।
वास्तविक ज्ञान
ईश्वरीय मार्गदर्शन के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान है। दूसरी ज्ञान शाखाएँ चाहे वे आनुभविक हों या अन्तर-परक, उनकी हैसियत मूल ज्ञान के साक्ष्यों की है। नैतिकता का अध्ययन हमें बताता है कि जीवन के नियम, बुद्धि और अन्तर्ज्ञान और मानव के अनुभव, ये सब ईश्वरीय मार्गदर्शन के सत्य और कल्याणप्रद होने के साक्षी हैं। मूल मानदण्ड ईश्वरीय मार्गदर्शन है। दार्शनिकों और तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तावित चीज़ों का इससे निषेध नहीं होता, बल्कि इससे उनका सुधार होता है और वे पूर्ण भी होती हैं। उनमें से यदि कोई अमर्यादित हो गई है तो ईश्वरप्रदत्त मार्गदर्शन में उसे एक समुचित व्यवस्था के अन्दर उसके अपने ठीक स्थान पर रखा गया है।
यह विचार सर्वथा असत्य है कि इस्लाम में नैतिकता केवल स्वर्ग और नरक की धारणा पर निर्भर करती है। स्वर्ग और नरक की धारणा नैतिकता का मूलाधार नहीं बल्कि यह नैतिकता की अन्तिम परिणति है। इस बात को एक मिसाल से समझा जा सकता है। अगर किसी से कहा जाए कि किसी का माल हड़प करोगे तो जेल जाना पड़ेगा तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि इस काम की बुराई कारावास पर निर्भर करती है स्वयं इस काम में कोई बुराई नहीं? इसी तरह अगर किसी से कहा जाए कि सच्चाई अपनाने वाले को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो क्या इसका यह अर्थ लेना सही हो सकता है कि सच्चाई का आधार प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, सच्चाई अपने अन्दर कोई मूल्य और महत्व नहीं रखती?
क़ुरआन ने भलाई और बुराई की ऐसी धारणा प्रस्तुत की है, जिस की उच्चता की कल्पना भी साधारण मन नहीं कर सकता। क़ुरआन भलाई को 'मारूफ़' कहता है अर्थात उसकी दृष्टि में भलाई वह है जिससे मानव की प्रकृति भली-भाँति परिचित है, जो उसके स्वभाव के ठीक अनुकूल है, जिसे वह पहचानती है। बुराई को क़ुरआन, 'मुनकर' कहता है। अर्थात बुराई उसकी दृष्टि में वह है जिसे मानव स्वभाव नकारता है, जो मानव-प्रकृति के लिए अपरिचित है, जिसको वह जानती नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस्लाम में भलाई और बुराई का आधार मानव प्रकृति और स्वभाव है। उसकी दृष्टि में अच्छाई यह है कि प्रकृति के अनुरूप ठीक-ठीक चला जाए। अभीष्ट यह है कि आदमी उन्नति करके उस उच्च स्थान को प्राप्त कर ले जहाँ धर्म की कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नज़र न आए। सब कुछ उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हो। स्वर्ग के बारे में क़ुरआन में कहा गया है :
“तुम्हारे लिए वहाँ सभी कुछ है जो तुम्हारा जी चाहे, और वहाँ तुम्हारे लिए वह सभी कुछ है जिसकी इच्छा तुम्हारे अन्दर हो।” (41:31)
इस्लामी दृष्टिकोण से प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने का नाम बुराई है और इसका अंजाम यह होता है कि मनुष्य पतन और विघटन के उस स्थल तक पहुँच जाता है जहाँ कोई चीज़ प्रिय और वांछित न पाई जाए। जो कुछ भी हो उसकी मर्ज़ी के प्रतिकूल हो। नरक एक ऐसा ही स्थान है जिस तक आदमी को उसकी नैतिक गिरावट ही पहुँचाती है। इससे मालूम हुआ कि नैतिकता का मूलाधार मानव का अपनी प्रकृति को पहचानना और उसके अनुरूप आचरण करना है। नैतिकता कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि वह मानव प्रकृति और स्वभाव की सही अभिव्यक्ति है। मानव अगर अपनी वास्तविक भावनाओं और अनुभूतियों को पहचान ले तो नैतिक अनिवार्यताएँ उसके अपने दिल की उमंगों से भिन्न कोई चीज़ नहीं हैं। जब तक मानव अपनी वास्तविक प्रकृति से परिचित नहीं होता वह बुराई से चाहे बच भी जाए मगर उसके दिल और दिमाग़ पूर्ववत गुनाहगार रहेंगे।
जैसा व्यक्तित्व वैसा ही कर्म
आदमी का जैसा व्यक्तित्व होता है उससे कर्म भी वैसे ही होते हैं। किसी कर्म के पीछे केवल नैसर्गिक प्रेरणाएँ (Motives) ही कार्यरत नहीं होतीं बल्कि उसमें उसका मन-मस्तिष्क, विचार और बुद्धि भी कार्य करती है। उसके पीछे उसके आदर्श और जीवनोद्देश्य का भी हाथ होता है जिसे वह चेतन या अचेतन रूप से अपनाए हुए होता है। इस दृष्टि से व्यक्ति का चरित्र और नैतिकता उसके जीवन का कुछ भाग, या एम. आर्नल्ड (Mathew Arnold) के अनुसार तीन चौथाई ही नहीं होता बल्कि स्वाभाविक रूप से वह उसके सम्पूर्ण जीवन पर छाया हुआ होता है।
इस्लामी दृष्टिकोण से परोक्ष की कुछ ऐसी चीज़ें भी नैतिकता के लिए प्रेरकों का काम करती हैं जिनका एहसास आम लोगों को नहीं होता। आदमी जब अपने जीवन और परोक्ष के विस्तृत लोक के मध्य, जो यथार्थ जगत् है, अनुकूलता पैदा कर लेता है तो ईश्वर की ओर से उसे सहयोग और सहायता प्राप्त होने लगती है। उसे ज्ञान और तत्वदर्शिता प्रदान की जाती है। उसे पारितोष और शान्ति प्राप्त होती है। फ़रिश्ते भी उसके हृदय में अच्छे विचारों और भावों को डालने लगते हैं और वह महसूस करने लगता है कि ईश्वर की एक उच्चतम और पवित्र मख़्लूक़ (सृष्टजीव) का संग-साथ भी उसे प्राप्त है।
नैतिकता की अभिव्यक्ति
मानव-जीवन में नैतिकता की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हक़ अदा करने के रूप में होती है। नैतिक दृष्टिकोण से मानव पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ और अधिकार उसके सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता प्रभु का है। ईश्वर के हक़ को अदा करने में उसकी उपासना, पूजा, आज्ञापालन आदि सारी बातें सम्मिलित हैं। ईश्वर के बाद उसके बन्दों के हक़ हैं जिनसे उसके विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। ईश्वर के बन्दों में सर्वाधिक सुस्पष्ट हक़ माता-पिता का होता है, क्योंकि माता-पिता से मानव का सम्बन्ध अत्यन्त क़रीबी और गहरा होता है। फिर क्रमिक रूप से दूसरे लोगों के हक़ सामने आते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ विवरण क़ुरआन की इस आयत में मिलते हैं—
“अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ। और अच्छा व्यवहार करो, माता-पिता के साथ, नातेदारों, अनाथों और मुहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ रहनेवाले व्यक्ति के साथ और मुसाफ़िर के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो।" (4:36)
इस आयत में माता-पिता, नातेदारों और दूसरों के साथ सद्व्यवहार का आदेश देते हुए ईश्वर की बन्दगी का आदेश दिया गया है। इसमें इस बात का इशारा पाया जाता है कि जिस प्रकार माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों आदि के साथ सद्व्यवहार मानव के लिए एक नैतिक और स्वाभाविक बात है ठीक उसी प्रकार ईश्वर के आज्ञापालन और उसकी बन्दगी की मांग भी एक स्वाभाविक और प्राकृतिक माँग है जिसका मानवीय नैतिकता से गहरा सम्बन्ध है। दोनों प्रकार के हक़ों को अदा करने में एक ही आधारभूत नैतिक नियम कार्यरत है। इनमें से किसी एक की उपेक्षा करना उस आधारभूत नियम का निषेध है और इससे मानव स्वयं अपनी नैतिकता और चरित्र को भी आघात पहुँचाता है। आधारभूत नैतिक नियम जीवन के समस्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक।
इन विवरणों के प्रकाश में इस बात का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि नैतिक दायित्वों का निर्वाह मात्र किसी बाह्य क़ानून के अनुपालन का नाम नहीं है और न ही यह आदमी का कोई ऐसा त्याग है जो किसी अजनबी (Alien) सत्ता के लिए हो, बल्कि यह तो जीवन के उन अवयवों की प्रकृति के साथ हमारे समन्वय मात्र की अभिव्यक्ति है जिनसे मानव चरित्र का निर्माण होता है। अतएव प्लेटो ने कहा है :
"Virtue will be a kind of health and beauty and good habit of the soul; and vice will be a Disease and Diformity and Sickness of it. (Plato)
“नेकी को स्वास्थ्य और एक प्रकार का सौन्दर्य और आत्मा की एक अच्छी वृत्ति कहा जाएगा और गुनाह को रोग और आत्मा का बिगाड़ और उसकी बीमारी कहेंगे। (G. Lowes Dickinson)
सच है, नेकी की तलाश और गुनाहों से बचना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई स्वास्थ्य का इच्छुक हो और बीमारी से बचने का प्रयास कर रहा हो।
(2)
नैतिकता और इस्लाम
इस्लाम में नैतिकता का महत्व
(1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने मुझे नैतिक गुणों और अच्छे कामों की पूर्ति के लिए भेजा है।" (हदीस शरहुस-सुन्नह)
व्याख्या : मुवत्ता इमाम मालिक की एक हदीस है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं सुशीलता को पराकाष्ठा तक पहुँचाऊँ।”
मुसनद अहमद में यह हदीस हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित की हुई मिलती है।
इन हदीसों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक बड़ी वास्तविकता को प्रकट किया है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं कि मेरे भेजे जाने का अस्ल मक़सद नैतिकता और कर्म की अच्छाइयों और ख़ूबियों को पूर्णता तक पहुँचाना है। नैतिकता वस्तुतः स्वाभाविक भावों और अनुभूतियों ही का दूसरा नाम है। अपनी यथार्थता की दृष्टि से यह एक अदृश्य चीज़ है। यह आदमी के विभिन्न क्रियाकलापों और कार्यों के द्वारा प्रकट होती रहती है। इच्छा, वश, भावनाओं और अनुभूतियों के सही और बेहतरीन इस्तेमाल से उस जीवन का आविर्भाव होता है जिसे हम आदर्श और प्रिय जीवन कहते हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अस्ल कारनामा यही है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मानव जीवन की विभिन्न इकाइयों में विभक्त करने की अपेक्षा उसे अखण्ड रूप दिया और जीवन के प्रत्येक पहलू और उसके प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित, चाहे उसका सम्बन्ध सामाजिकता एवं अर्थ-व्यवस्था से हो या शासन और राजनीति से, नैतिकता के सही उसूल और नियम बताए। इन्हें व्यावहारतः जीवन में बरत कर दिखाया और इन्हीं उसूलों पर समाज और राज्य की व्यवस्था स्थापित की।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन में, 'मैं सुशीलता को पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिए भेजा गया हूँ' मानव जीवन की एक ऐसी व्याख्या निहित है जो सत्य भी है और सर्वोत्तम भी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नैतिकता को घिसी-पिटी और सीमित सोच से मुक्त करके उसे विस्तृत अर्थ दिया और उसको सार्वभौमिकता प्रदान की। यहाँ तक कि मानव के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का कोई हिस्सा भी नैतिकता से अलग और स्वतन्त्र न रहा और जीवन उस उसूल व नियम के अनुरूप हो गया जो उसूल और नियम हमें ब्रह्माण्ड में कार्यरत दिखाई देता है और जिसकी मूल आत्मा क़ुरआन के शब्दों में यह है—
“अल्लाह की तसबीह (महिमागान) कर रही है प्रत्येक वह चीज़ जो आकाशों में है और प्रत्येक वह चीज़ जो ज़मीन में है। उसी की बादशाही है और उसी के लिए प्रशंसा है, और उसे प्रत्येक चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।" (64:1)
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें सबसे अधिक मुझे वे लोग प्रिय हैं जो तुममें नैतिकता की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : तिर्मिज़ी में हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें से सबसे अधिक मुझे वे लोग प्रिय हैं और क़ियामत के दिन उन्हीं की बैठक भी मुझसे अधिक निकट होगी जो तुममें शील-स्वभाव की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं। और तुममें सबसे अधिक अप्रिय और क़ियामत के दिन मुझसे सबसे दूर रहनेवाले वे लोग हैं जो ज़्यादा बातें बनानेवाले, या वाक्चातुर्य में कुशल और बनावटी बातें करनेवाले अहंकारी हैं।"
मनुष्य वास्तव में एक नैतिक अस्तित्व है। उसके अच्छे या बुरे होने का वास्तविक मानदण्ड उसका शील-स्वभाव ही है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का विशेष सामीप्य और प्रेम उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो शील-स्वभाव की दृष्टि से अच्छे और उच्च होंगे। और इसमें सन्देह नहीं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का प्रेम और सामीप्य सफलता का स्पष्ट प्रतीक है।
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें सबसे अच्छे वे लोग हैं जो नैतिकता की दृष्टि से तुममें सबसे अच्छे हैं।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : ज्ञात हुआ कि जीवन का मूल्य निश्चित करने में वास्तविक निर्णायक चीज़ नैतिकता है। इसलिए मुबारक हैं वे लोग जो नैतिकता की दृष्टि से अपने को अच्छी से अच्छी हालत में देखने की कामना मन में संजोए रखते हैं।
(4) मुज़ैना क़बीले के एक व्यक्ति से उल्लिखित है कि लोगों ने पूछा—
ऐ अल्लाह के रसूल! इनसान को जो कुछ प्रदान किया गया है, उसमें सबसे उत्तम क्या है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उत्तर दिया : "सुशीलता।" (हदीस : बैहक़ी, बग़वी)
व्याख्या : सुशीलता अपने बाह्य पक्ष और परिणामों की दृष्टि से अल्लाह की एक बड़ी देन है। सुशीलता में जो आकर्षण और सौन्दर्य पाया जाता है उसे किसी और चीज़ में सोचा तक नहीं जा सकता। शील-स्वभाव में जो शक्ति और प्रभाव निहित है वह किसी चमत्कार (Miracle) में भी नहीं है। इससे शत्रुओं का दिल भी जीता जा सकता है। एक सत्य के आमन्त्रणदाता और सन्मार्ग की ओर बुलानेवाले के जीवन में तो नैतिकता का सर्वाधिक महत्व होता है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की करुणा और नर्मदिली को क़ुरआन ने अल्लाह की दया कहा है। 'नुबूवत' (पैग़म्बरी) के काम को अंजाम देने में इस नैतिक गुण का जो महत्व है उसपर भी क़ुरआन ने रौशनी डाली है। कहा गया है—
“(ऐ नबी!) यह अल्लाह की दयालुता है कि तुम लोगों के लिए नर्म हो, यदि तुम क्रूर और कठोर हृदय वाले होते तो ये सब तुम्हारे पास से छँट जाते। तुम उन्हें क्षमा कर दो और उनके लिए क्षमा चाहो और दीन (धर्म) के काम में उनसे भी परामर्श कर लिया करो।" (3:159)
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“मोमिन अपनी सुशीलता से उन लोगों का दर्जा प्राप्त कर लेता है जो रात में (अल्लाह के समक्ष) खड़े रहते हों और दिन को सदैव रोज़ा रखते हों।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मतलब यह है कि सुशीलता एक ऐसा अभीष्ट गुण है जिससे बहुत-सी कमियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि अपने नैतिक गुण के द्वारा आदमी उस व्यक्ति के दर्जे और पद को भी प्राप्त कर लेता है जो रातों में अल्लाह की इबादत करता और दिन में रोज़े रखता है। सुशील मोमिन यथार्थतः सदैव अल्लाह के आज्ञापालन और बन्दगी की हालत में होता है। उसकी आत्मा की पवित्रता और सुशीलता उसे सदैव उच्च दर्जे की आध्यात्मिकता और उच्च कोटि के चरित्र से जोड़े रखती है।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि अधिकतर लोग किसके कारण जन्नत में प्रवेश करेंगे? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईशभय और सुशीलता के कारण।"
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि अधिकतर लोग किसके कारण दोज़ख़ (नरक) में प्रवेश करेंगे? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ज़ुबान और शर्मगाह (गुप्तांग) के कारण।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : जन्नत में अधिकतर लोग अपनी सुशीलता और अल्लाह से डर रखने के कारण जाएँगे। ज़बान और शर्मगाह की असुरक्षा और उन गुनाहों के कारण जो इन दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, अधिकतर लोग दोज़ख़ में डाले जाएँगे। जो लोग ज़बान और शर्मगाह की सुरक्षा का ख़्याल रखेंगे, आशा है कि उनकी पूरी ज़िन्दगी साफ़-सुधरी और पाक होगी।
(7) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया, जबकि वह व्यर्थ (अर्थात् त्याज्य) ही है, उसके लिए जन्नत के (अन्दर) किनारे के स्थान पर मकान बनाया जाएगा। और जिस किसी ने झगड़ना छोड़ दिया जबकि वह हक़ (सत्य) पर था, उसके लिए जन्नत के मध्य में मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपने शील-स्वभाव को उत्तम बना लिया, उसके लिए जन्नत की ऊँचाइयों पर मकान बनाया जाएगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी, शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : इस हदीस से भी मालूम होता है कि जीवन में सुशीलता को आधारभूत महत्व प्राप्त है। जिन लोगों का जीवन सुशीलता और नैतिक गुणों से सुशोभित होगा उन्हें जन्नत के उच्च वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि वास्तव में ऊँचे दर्जे के लोग वही हो सकते हैं जो नैतिक दृष्टि से उत्तम हों।
(8) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन मोमिन की तुला में जो सबसे भारी चीज़ होगी वह सुशीलता है।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : सुशीलता चूँकि जीवन का वास्तविक सौन्दर्य और मौलिक मानव-चरित्र है, इसलिए स्वाभाविक बात है कि कर्म-तुला में वही सबसे अधिक भारी होगी। आदमी की पहचान इससे कदापि नहीं होती कि उसके पास सुख-सुविधा के क्या सामान हैं, बल्कि आदमी की असल पहचान इससे होती है कि वह स्वयं क्या है? अल्लाह के यहाँ मूल प्रश्न यह नहीं होगा कि मानव ने संसार में कितना धन संग्रह किया और कितनी ख्याति प्राप्त की, अपितु प्रश्न यह होगा कि वह अल्लाह के पास कैसा व्यक्तित्व लेकर आया है। व्यक्तित्व का निर्माण आदमी के विचार, कर्म और नैतिक गुणों ही के द्वारा होता है। आदमी अगर नैतिक दृष्टि से पतित है तो चाहे वह संसार का सबसे धनी और सत्ताधारी व्यक्ति हो, वास्तव में वह एक निर्धन और निकृष्ट जीव है।
(9) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“न तदबीर के सदृश कोई बुद्धि है और न बुराई से बचने के सदृश कोई ईशभय है और न सुशीलता के सदृश कोई कुलीनता पाई जाती है।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि उस बुद्धि के सदृश कोई बुद्धि नहीं जिसके साथ तदबीर हो। आदमी परिणाम पर नज़र रखे और विकृतियों के प्रति असावधान न हो। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि से काम तो लेता है किन्तु इतना नहीं कि परिणाम को देख सके तो उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता उसे तबाह होने से नहीं बचा सकती।
धर्म में जिन बातों का आदेश दिया गया है और जिन बातों से रोका गया है इन दोनों ही का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन कुछ पहलुओं से निषिद्ध चीज़ों से दूर रहने का महत्व आदेशों के पालन से बढ़कर है। इसकी मिसाल बिलकुल ऐसी है जैसे बीमारी की हालत में दवा के मुक़ाबले में परहेज़ करने का महत्व अधिक होता है।
इस हदीस से यह भी ज्ञात हुआ कि वास्तविक श्रेष्ठता और श्रेय की चीज़ सुशीलता है। यदि यह नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है।
(10) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहा करते थे—
“ऐ अल्लाह, तूने मेरी संरचना को सुन्दर बनाया, तो मेरे स्वभाव को भी सुन्दर बना दे।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात् जिस प्रकार तूने मेरे बाह्य रूप को अच्छा बनाया है उसी प्रकार मुझे आन्तरिक और नैतिक उत्तमता भी प्रदान कर। नैतिक गुणों के अभाव में मनुष्य के बाह्य अस्तित्व का कोई मूल्य शेष नहीं रहता।
(11) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या मैं तुम्हें यह न बताऊँ कि तुममें अच्छे लोग कौन हैं?” लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, आप अवश्य बताएँ, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुममें अच्छे लोग वे हैं जो दीर्घायु और सुशील हैं।" (हदीस : अहमद)
व्याख्या : आयु यदि दीर्घ है तो आदमी को अधिक से अधिक नेक काम और अल्लाह के आज्ञापालन और उसकी बन्दगी कर सकने के अवसर भी अधिक प्राप्त होते हैं।
मानवीय नैतिक गुण
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
‘‘लोग उन सौ ऊँटों के सदृश हैं जिनमें मुश्किल से तुम किसी को सवारी के योग्य पा सको।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात् जिस प्रकार ऊँटों की एक बड़ी संख्या में अपने मतलब का ऊँट सरलता से नहीं मिलता, ठीक यही स्थिति मनुष्यों की भी है। आदर्श पुरुष और मानवीय गुणों से युक्त लोग कम ही मिलते हैं। यह बात अगर हमारे सामने रहे तो हम इस परिस्थिति से कभी हतोत्साहित नहीं होंगे कि ज़्यादा-से-ज़्यादा अच्छे और विश्वसनीय लोग क्यों नहीं मिलते। ऐसे लोग होते ही कम हैं, किन्तु कुछ व्यक्ति भी काम के हाथ आ जाएँ तो वे एक बड़ी संख्या पर भारी होंगे। उनके द्वारा बड़े से बड़ा कार्य सम्पन्न हो सकता है। मानव इतिहास भी इसी का साक्षी है।
मानवीय नैतिक गुणों और मानवीय प्रतिभाओं में इस्लाम चार चाँद लगा देता है। इस्लाम के प्रकाश में वे चमक उठती हैं। मनुष्य के भीतर जो भी ख़ूबियाँ और अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, उनके उचित प्रयोग से ही वह सफलता की ऊँचाई तक पहुँच सकता है।
इस हदीस से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यथार्थप्रियता विदित होती है। मोमिन का कर्तव्य है कि वह दुनिया में तथ्यों की उपेक्षा करते हुए कदापि अपना जीवन व्यतीत न करे।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि लोगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ और आदरणीय कौन है? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो उनमें सबसे ज़्यादा (अल्लाह का) डर रखता हो।"
लोगों ने कहा कि हम आप से इसके विषय में नहीं पूछ रहे हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सर्वाधिक श्रेष्ठ और सम्मानित यूसुफ़ हैं, जो नबी हैं, उनके बाप भी नबी थे और दादा भी नबी थे और परदादा (नबी ही नहीं बल्कि) अल्लाह के घनिष्ठ मित्र थे।"
लोगों ने कहा कि हम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इस विषय में नहीं पूछ रहे हैं? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छा तुम अरब खदानों के बारे में पूछ रहे हो? उनमें जो अज्ञानकाल में अच्छे थे वही इस्लाम में भी सबसे अच्छे हैं, जबकि (धर्म के विषय में) वे समझ प्राप्त कर लें।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मनुष्यों की उपमा खदानों से दी गई है। जिस प्रकार खान में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, यहाँ तक कि लोहा, कोयला आदि के अतिरिक्त सोने और चाँदी की खानें भी पाई जाती हैं। यही स्थिति मनुष्यों की भी है। जहाँ एक ओर उत्तम और सम्माननीय मनुष्य हमें मिलते हैं, वहीं ऐसे लोगों से भी प्रायः मिलना होता है जिनसे मानवता का सिर लज्जा से झुक जाए।
जो लोग अज्ञानकाल में साहसी, वीर, त्यागी, उत्साही, विशाल हृदय और ज़िन्दादिल अर्थात् मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे, वही इस्लाम में भी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, जबकि इस्लाम की उन्हें सही समझ प्राप्त हो जाए। गिरे हुए और निरुत्साहित लोग न तो अज्ञान और असत्य के काम के हो सकते हैं और न इस्लाम का बोलबाला करने और मानवता की सेवा में उनका कोई विशेष योगदान हो सकता है।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम लोगों को खदानों (खनिज पदार्थों की खानों) के सदृश पाओगे। इनमें जो अज्ञानकाल में अच्छे थे, वे इस्लाम में भी अच्छे हैं, जबकि वे (धर्म के विषय में) समझ हासिल कर लें। और तुम इस मामले (इस्लाम) में लोगों में सबसे अच्छा उसको पाओगे जिसको इससे सबसे अधिक घृणा थी। और तुम लोगों में सबसे बुरा उसे पाओगे जो दो रुख़ा हो, इन लोगों के पास जाता हो तो एक मुँह के साथ और उनके पास पहुँचता हो तो दूसरे मुँह के साथ।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : कुफ़्र की हालत में जिसे इस्लाम से कठोर घृणा और शत्रुता थी और इस्लाम को मिटाने के प्रयास में जो व्यक्ति अग्रसर रहा है, वही ईमान लाने के पश्चात् इस्लाम के प्रेम में सबसे अधिक डूबा हुआ दिखाई देता है। उस व्यक्ति से इस्लाम की महान सेवाओं की आशा की जा सकती है। जिस व्यक्ति के अन्दर शत्रुता की सामर्थ्य ही न हो उसके अन्दर मित्रता का गुण कहाँ से आ जाएगा?
दोरुख़ापन, जिसका स्पष्टीकरण इस हदीस से किया गया है, पतित आचरण की अत्यन्त घिनौनी और बुरी स्थिति है। जो व्यक्ति आचरण और नैतिकता की इस गिरी हुई अवस्था तक पहुँच गया हो उसके विषय में यह समझ लेना चाहिए कि वह समाज का एक अत्यन्त अप्रिय तत्त्व है। उससे उपद्रव और बुराई के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार के लोगों की सारी दौड़-धूप के पीछे फ़रेब और छल-कपट के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इस प्रकार के लोगों से सावधान रहना आवश्यक है। शिथिल और उत्साहहीन लोग न अज्ञानता और असत्य के काम के होते हैं और न इस्लाम की बुलन्दी और मानवता की सेवा में इनका कोई विशेष योगदान हो सकता है।
(4) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अन्तिम वसीयत जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझे की, जबकि मैं रिकाब में पाँव रखने लगा था, वह यह थी—
"ऐ मुआज़-बिन-जबल! अपने स्वभाव को लोगों के लिए सबसे अच्छा रखना।" (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : अर्थात् लोगों के साथ तुम्हारी नीति उच्च कोटि की नैतिकता के अन्तर्गत होनी चाहिए। ईमानवाले की हैसियत सदैव एक उत्तरदायी व्यक्ति की होती है। उसे अपने ईमान के दायित्व से किसी स्थिति में भी मुक्त नहीं ठहराया जा सकता।
नैतिकता का सम्बन्ध ईमान से
(1) हज़रत अबु-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईमानवालों में ईमान की दृष्टि से सबसे पूर्ण व्यक्ति वह है जो उनमें नैतिक गुणों की दृष्टि से सबसे अच्छा है। और तुममें अच्छा वह है जो अपनी स्त्रियों के लिए अच्छा हो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस से स्पष्ट है कि ईमान और नैतिकता में घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता है। मोमिन या ईमानवाले व्यक्ति के शील-स्वभाव और उसके व्यावहारिक जीवन में वस्तुतः उसके ईमान और उसकी आस्था ही की अभिव्यक्ति होती है। आदमी का ईमान यदि पूर्ण और सुदृढ़ होगा तो अनिवार्यतः उसकी नैतिक दशा भी सबसे अच्छी होगी। आदमी के अच्छे होने का स्पष्ट लक्षण यह है कि वह अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। स्त्रियों को कमज़ोर समझकर सामान्यतः लोग उनके साथ अत्याचारपूर्ण नीति अपनाते हैं। इतिहास के प्रत्येक काल में औरतों पर साधारणतया अत्याचार होता रहा है। स्त्री यदि पुरुष के संरक्षण में दी गई है तो इसलिए नहीं कि वह पुरुष के अत्याचारों का निशाना बने, बल्कि समाज के निर्माण और उसकी भलाई एवं कल्याण के लिए आवश्यक था कि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहना स्वीकार करे। इस्लाम ने समाज में एक ओर स्त्री के स्थान को ऊँचा किया, दूसरी ओर उसने औरतों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ली। इसका इनकार वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसने इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया हो।
(2) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति ने प्रेम किया अल्लाह के लिए, शत्रुता की अल्लाह के लिए, दिया अल्लाह के लिए, और रोका (अर्थात् न दिया) अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को पूर्ण कर दिया।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात् पूर्ण ईमान यह है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, वांशिक और जातीय पक्षपातों से मुक्त हों। जीवन में हम जो नीति भी अपनाएँ, उसमें मूलतः अल्लाह की प्रसन्नता की प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट हो। मित्रता हो या शत्रुता, देना हो या रोकना हमारा सब कुछ अल्लाह ही के लिए हो। पूर्ण समर्पण के अभाव में अल्लाह पर ईमान लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति दावा तो यह करता हो कि वह गौरववान और सर्वश्रेष्ठ अल्लाह पर ईमान रखता है, परन्तु ज़िन्दगी के मामलों में वह अल्लाह के आदेशों और उसकी पसन्द एवं नापसन्द की प्रायः अनदेखी करता चला जाए, तो उसके विषय में यही कहा जाएगा कि वह या तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखता या रखता है तो उसका ईमान अपूर्ण और कमज़ोर है, और अभी उसका ईमान उसके जीवन में प्रेरक शक्ति बनकर नहीं उभर सका है। उसकी यह दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है।
मुसनद अहमद की एक रिवायत में इसी प्रकार की एक हदीस के अन्त में ये शब्द भी आए हैं—
“अतः जब अल्लाह ही के लिए उसका प्रेम और अल्लाह ही के लिए उसकी शत्रुता और नफ़रत हो तो वह इसका पात्र हो जाता है कि अल्लाह उसे अपने संरक्षण में ले।”
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सौगन्ध है उस सत्ता की जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं! तुम जन्नत में प्रवेश न पाओगे जब तक कि ईमान न लाओ, और तुम ईमानवाले न होगे जब तक कि तुम परस्पर एक-दूसरे से प्रेम न करो। क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बताऊँ कि यदि तुम उसे व्यवहारतः अपना लो तो परस्पर तुम्हारे बीच प्रेम उत्पन्न हो जाए। आपस में सलाम को रिवाज दो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह हदीस सहीह मुस्लिम में भी लगभग इन्हीं शब्दों के साथ मिलती है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने लोगों को सावधान किया है कि यदि वे अल्लाह के सामीप्य और उसकी जन्नत के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने जीवन में सामान्य रीति से हटकर एक विशेष कार्य शैली अपनानी होगी। इसमें सन्देह नहीं कि जन्नत की प्राप्ति जीवन का एक उच्च उद्देश्य है। लेकिन जन्नत में प्रवेश ईमान के बिना सम्भव नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का पेट मक्खी को ग्रहण करने से इनकार कर देता है, यदि बेख़बरी में कोई मक्खी पेट में चली जाती है, तो तुरन्त उबकाई आती है और क़ै के द्वारा आमाशय मक्खी को बाहर फेंक देता है, ठीक इसी प्रकार जन्नत की पवित्रता और विमलता ईमान न रखनेवाले अपवित्र व्यक्ति को कदापि ग्रहण न कर सकेगी। अतः मनुष्य यदि अपनी स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति अर्थात् जन्नत प्राप्त करना चाहता है तो वह स्वयं को जन्नत के योग्य बनाए। इसके लिए आवश्यक है कि वह कुफ़्र (इनकार) को छोड़कर ईमान ले आए। और ईमान से अभिप्रेत किसी विशेष दृष्टिकोण या आस्था की केवल ज़बानी स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि अभीष्ट ईमान यह है कि वह जीवन में एक स्पष्ट गुण के रूप में परिलक्षित हो। ईमान की अपेक्षा यह है कि हम एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक व्यवहार करें। हमारे बीच वास्तविक सम्बन्ध प्रेम का हो। पारस्परिक प्रेम उत्पन्न करनेवाली कई चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से इसके लिए एक प्रभावकारी साधन यह है कि हम समाज में सलाम को अधिक से अधिक प्रचलित करने की कोशिश करें। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति अपने भाई के पास से गुज़रे तो उससे अपने सम्बन्ध को प्रकट किए बिना यूँ ही अपरिचित व्यक्ति की तरह गुज़र जाए। ऐसी अपरिचितता की आशा तो किसी पुष्पवाटिका के पुष्पों से भी नहीं की जाती। वे तो अपने निकट से गुज़रनेवालों तक अपनी सुगन्ध पहुँचा ही देते हैं।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"उस सत्ता की सौगन्ध जिसके क़ब्ज़े में मेरे प्राण हैं! तुममें से कोई ईमान लानेवाला न होगा जब तक कि मैं उसके लिए उसकी सन्तान और उसके पिता और सभी लोगों से बढ़कर प्रिय न हो जाऊँ।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा, “अल्लाह की सौगन्ध, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे प्रत्येक चीज़ से बढ़कर प्रिय हैं सिवाए अपने प्राण के।" इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "नहीं, ऐ उमर! (तुम ईमानवाले नहीं हो सकते) जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय न हो जाऊँ।” हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा, "अल्लाह की क़सम! आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अब ऐ उमर! (तुम ईमानवाले हो)।”
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम रखना अल्लाह के प्रेम ही के कारण अनिवार्य है। अल्लाह से प्रेम वस्तुतः धर्म, ईमान और सभी कर्मों का मूल है। जो कर्म अल्लाह के लिए न हो या जिसके पीछे अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने की भावना सक्रिय न हो, तो यह स्वीकार्य नहीं है। इसी लिए सहीह हदीस में आता है कि ऐसा क़ारी (पाठक) या मुजाहिद (अल्लाह की राह में जिहाद करनेवाला) या सदक़ा करनेवाला जहन्नम में प्रविष्ट होगा जो दिखावा करने वाला हो। इबादत, अल्लाह की तरफ़ रुजू होना और उसी के प्रति एकाग्रता आदि वास्तव में अल्लाह से प्रेम ही में सम्मिलित है। अल्लाह ने प्राणियों को पैदा ही इसलिए किया है कि वे उसकी इबादत करें (क़ुरआन:56)। अर्थात् अल्लाह से आत्यन्तिक प्रेम करें और उसे हृदय और प्राण से बढ़कर प्रिय समझें। लेकिन ईश्वर की महानता के एहसास के बिना यह प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। इसी लिए इबादत और आत्यन्तिक प्रेम में आत्यन्तिक विनयशीलता का भाव भी सम्मिलित है।
प्रेम ही जीवन की मूल-निर्णायक चीज़ है। और यही चीज़ आख़िरत में भी निर्णायक सिद्ध होगी। अतएव अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पवित्र वचन है कि “आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसे प्रेम होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
जीवन का मौलिक उद्देश्य और अभिप्राय अल्लाह से प्रेम ही है। दूसरे लोगों से प्रेम सम्बन्ध अल्लाह से प्रेम के कारण ही स्थापित होता है। इस प्रकार निकट सम्बन्धियों, मित्रों और नातेदारों के प्रेम को एक ऐसा आधार मिल जाता है जिसके कारण यह प्रेम भी न केवल यह कि सुदृढ़ हो जाता है, बल्कि विवेकशील व्यक्ति की दृष्टि में अर्थपूर्ण भी हो जाता है।
प्रेम अपने व्यक्तित्व की परिधि से निकलने को कहते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने ही इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहता है और जिसकी भाग-दौड़ केवल अपने ही लिए होती है, वह प्रेम शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ रहता है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सबसे बढ़कर प्रेम करने का तात्पर्य यह होता है कि मोमिन के हार्दिक लगाव का केन्द्रबिन्दु अपने आप से कहीं अधिक अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का व्यक्तित्व होता है। यह चीज़ उसे प्रत्येक प्रकार की संकीर्णता से मुक्त करती है और उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ उसे कोई पराया नहीं दिखाई पड़ता है। अब अपनी ही नहीं सारी मानवता की भलाई और उसका कल्याण उसके समक्ष होता है। मानवता की हर मूल्यवान निधि उसकी अपनी निधि होती है। इस प्रकार लोगों की कठिनाइयाँ उसकी अपनी कठिनाइयाँ बन जाती हैं। क्योंकि जिस रसूल को वह अपने प्राण से बढ़कर प्रिय समझता है, वह सारे जगत् का शुभ-चिन्तक और हितैषी है। फिर कैसे सम्भव है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम का सम्बन्ध उसे स्वार्थपरता, अवसरवादिता और प्रत्येक प्रकार के पक्षपात और भेदभाव से मुक्त न कर दे।
जब ईमानवाला व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपने प्राण से बढ़कर प्रिय रखता है तो उसे अल्लाह से कितना प्रेम होगा इसका अनुमान मनुष्य स्वयं कर सकता है। ईमान की यह दशा यदि हमारे अन्दर उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने में कोई चीज़ हमारे लिए रुकावट बन सकती है? कदापि नहीं।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईमान की सत्तर से कुछ अधिक शाखाएँ हैं। और लज्जा ईमान की एक शाखा है।" (हदीस : मुस्लिम)
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"कृपणता व लोभ और ईमान दोनों किसी बन्दे के हृदय में एकत्र नहीं होंगे।" (हदीस : नसई)
(7) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"उस सत्ता की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! बन्दा ईमानवाला नहीं होता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसन्द न करे जो वह स्वयं अपने लिए पसन्द करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : आदमी अपने लिए बुराई को नहीं बल्कि अच्छाई और भलाई को पसन्द करता है। इसलिए अनिवार्यतः उसे अपने दूसरे भाइयों के लिए भी अच्छाई और भलाई का इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में हमारा ईमान पूर्ण नहीं हो सकता। ईमान तो हमें प्रत्येक प्रकार की संकीर्णता से, चाहे वह हृदय की संकीर्णता हो या विचार और चिन्तन की संकीर्णता हो, निकालकर विशालहृदयता प्रदान करता है। यह विशालहृदयता शेष रहे यह उस भाव पर निर्भर करता है जिसे हम प्रेम कहते हैं।
(8) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह की क़सम! वह ईमानवाला नहीं हो सकता, अल्लाह की क़सम! वह ईमानवाला नहीं हो सकता, अल्लाह की क़सम! वह ईमानवाला नहीं हो सकता।" पूछा गया कि कौन ऐ अल्लाह के रसूल! (ईमानवाला नहीं हो सकता)? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "वह व्यक्ति जिसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से सुरक्षित न हो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात् यह उसके ईमान को अपेक्षित है कि मोमिन का पड़ोसी उससे किसी प्रकार के ख़तरे और आशंका का एहसास न करे, बल्कि वह उससे अपनी जान-माल और सम्मान को सुरक्षित पाए। मोमिन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी की इज़्ज़त और माल पर डाका डाल सकता है। वह तो लोगों की सुरक्षा और उनपर दया-दृष्टि करनेवाला होता है।
(9) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
"वह व्यक्ति मोमिन नहीं जो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रहे।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : मोमिन लोगों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होता है। पड़ोसी भूखा रह जाए और वह पेट भरकर मज़े लेकर खाए, ऐसी कठोर हृदयता का प्रदर्शन कोई ईमानवाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि कोई ईमान का दावेदार ऐसा कठोर हृदय और निर्दयी है तो उसे अपने ईमान की चिन्ता होनी चाहिए। आश्चर्य नहीं कि यह कमज़ोर और प्राणहीन ईमान भी उसके यहाँ ज़्यादा दिन तक न रह सके।
(10) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन भोला-भाला और सज्जन और दानशील होता है तथा फ़ाजिर आदमी चालाक (धूर्त), दुर्जन और कंजूस होता है।" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से यह मालूम हुआ कि ईमान का आदमी के आचरण और कर्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मोमिन सीधे-सादे स्वभाव का होता है। वह धूर्तता और छल-कपट का शिकार तो हो सकता है, लेकिन वह स्वयं किसी के साथ धूर्तता और छल-कपट की नीति नहीं अपना सकता। यह बात भी है कि ईमानवाले को बार-बार धोखा भी नहीं दिया जा सकता। अतएव हदीस में है—
"ईमानवाले व्यक्ति को एक सुराख़ से दो बार नहीं डसा जाता।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
ईमानवाला उदार होता है। उदारता का दूसरा नाम सज्जनता है। दानशीलता सज्जनता की सबसे बड़ी पहचान है। इसके विपरीत मिथ्याचारी से सज्जनता की आशा नहीं की जा सकती। वह दुर्जन ही होगा, जिसकी स्पष्ट पहचान कृपणता है। इस हदीस का सारांश यह है कि मोमिन सुशीलता और नैतिकता की प्रतिमूर्ति होता है और उल्लंघनकारी व्यक्ति बुरे स्वभाव का होता है। सज्जनता मोमिन का स्वभाव होता है। उसकी बुद्धि और विवेक से किसी बुराई और उपद्रव की सम्भावना नहीं रहती। वह अनजान और नासमझ नहीं होता, लेकिन उसकी बुद्धि और प्रतिभा अज्ञानता एवं चालबाज़ियों से पूर्णतः मुक्त होती है। इसके विपरीत एक उल्लंघनकारी व्यक्ति से किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती। वह लोगों को अपनी चालबाज़ियों से परेशानियों और उलझनों में डाल देता है। असज्जनता के सिवा किसी और चीज़ का प्रदर्शन वह नहीं कर सकता। भलाइयों के लिए उसका दामन हमेशा तंग ही रहेगा।
(11) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा और ईमान दोनों साथ रखे गए हैं। अतएव इनमें से जब एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत में ये शब्द आए हैं—
“अतएव इनमें से एक को छीन लिया जाता है तो दूसरा भी उसी के साथ चला जाता है।"
ईमान और नैतिकता में कितना गहरा सम्बन्ध होता है, इसका भली-भाँति अनुमान इस हदीस से किया जा सकता है। नैतिक गुणों में लज्जा को मौलिक महत्व प्राप्त है। अतएव अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"प्रत्येक धर्म का एक शील होता है। इस्लाम का शील लज्जा है।" (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
अर्थात् प्रत्येक धर्म का एक स्वभाव (Nature, Manner) होता है। इस्लाम के स्वभाव की सौम्यता और पवित्रता का इससे बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है कि लज्जा इसके स्वभाव का एक अंग है। लज्जा के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि ईमान से इसका गहरा और अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। ईमान और लज्जा में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इनमें कोई एक यदि शेष न रहे, तो दूसरा शेष नहीं रह सकता। एक के विदा होते ही दूसरा भी दम तोड़ देगा।
इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अपने ईमान को जाँचने-परखने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ईमान अपनी प्रकृति की दृष्टि से सदैव एक पवित्र जीवन में ढलने को तत्पर रहता है। जब तक वह एक पवित्र जीवन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर लेता उसे क़रार नहीं मिलता। जिस प्रकार किसी दूषित वातावरण में आदमी का दम घुटता है और वह ताज़ा हवा में साँस लेने को बेचैन हो जाता है, ठीक यही दशा ईमान की भी होती है। अब यदि हमारे जीवन से लज्जा और स्वाभिमान आदि नैतिक गुण लुप्त होते जा रहे हैं तो किसी को इस बात के समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि हमारे ईमान की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है।
(12) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“व्यभिचारी इस दशा में कि वह मोमिन हो व्यभिचार नहीं करता, न शराबी इस दशा में कि वह मोमिन हो शराब पीता है। और न चोर इस दशा में कि वह मोमिन हो चोरी करता है, और न उचक्का इस दशा में कि वह मोमिन हो कोई चीज़ उचकता है, जबकि लोग (विवशता की स्थिति में) उसकी ओर अपनी आँखें उठाते हैं।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात् जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है या शराब पीता है या वह चोरी करता है या लोगों के देखते-देखते किसी की कोई चीज़ उचकता है, तो उस समय वह मोमिन नहीं रह जाता। ईमान के स्थान पर उसके भीतर उस समय कोई दूसरी ही चीज़ काम कर रही होती है। जबकि होना यह चाहिए कि उसके सभी कर्म वे हों जो ईमान को अपेक्षित हैं। आदमी के जीवन में ईमान के स्थान पर कोई और शक्ति काम करने लग जाए तो यह इस बात का प्रमाण है कि ईमान उसके दिल में अभी पूरी तरह घर नहीं कर सका है, इसी लिए ईमान की विरोधी शक्ति को उसके जीवन में खेलने का अवसर प्राप्त हो जाता है।
(13) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो ईमान उसके भीतर से निकलकर उसके सिर पर सायबान की तरह ठहर जाता है। और जब वह यह काम कर चुकता है तो ईमान उसकी ओर पुनः लौट आता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ईमान जीवन की बहुमूल्य निधि है। गुनाह के समय आदमी का सम्बन्ध ईमान से टूट-सा जाता है। यह और बात है कि गुनाह के पश्चात् आदमी की वह मनोदशा शेष नहीं रहती जो गुनाह के समय होती है। गुनाह के पश्चात् आदमी को कठोर पश्चाताप होता है। वह अपने किए पर लज्जित होता है। ईश्वर से क्षमा याचना करता है। इस प्रकार गुनाह करने के बावजूद इसकी आशा शेष रहती है कि आदमी का दिल ईमान के वास्तविक भावों से फिर परिपूर्ण हो सके।
(14) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इब्ने-जुदआन अज्ञानकाल में नाते-रिश्ते का ध्यान रखता था और मुहताजों को खाना देता था, तो क्या यह उसके काम आएगा? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह उसके कुछ काम न आएगा, क्योंकि उसने किसी दिन भी यह न कहा कि मेरे रब, बदला दिए जाने के दिन मेरे गुनाह को क्षमा कर देना।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात् वह व्यक्ति कुफ़्र में ग्रस्त था, आख़िरत (पारलौकिक जीवन) पर उसका ईमान न था। इसलिए वह अल्लाह से नजात पाने का कभी इच्छुक न हुआ। ईमान के बिना चाहे कितने ही अच्छे कर्म हों, व्यर्थ सिद्ध होंगे। आख़िरत में वे आदमी के काम न आ सकेंगे। इससे मालूम हुआ कि अच्छे कर्म अल्लाह की दृष्टि में वही हैं जिनका वास्तविक प्रेरक ईमान हो, न कि कुछ और। ईमान के अभाव में वास्तव में वह जीवन ही नहीं प्राप्त होता जिसे मूल्यवान कहा जाए। जब किसी को अपेक्षित जीवन ही प्राप्त न हो तो उसके कर्म, विचार और नीति को कैसे मूल्यवान ठहराया जा सकता है।
(15) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि ईमान क्या है? तो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“नेकी करके जिसको ख़ुशी हो और बुराई करके जिसको दुख और पछतावा हो, तो वह मोमिन है।" (हदीस : हाकिम)
व्याख्या : इस हदीस से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि ईमान का इनसान के कर्म से घनिष्ट सम्बन्ध है। ईमान वस्तुतः आदमी की अभिरुचि और उसके स्वभाव को निखार देता है। ईमान का मूल आधार ही वास्तव में इनसान की सुरुचि और स्वाभाविक चेतनता है। इसी लिए मोमिन को नेकी से ख़ुशी और बुराई से कुढ़न होती है। इसके विपरीत ग़ैर-मोमिन व्यक्ति को अपने बुरे कर्म प्रिय और सुखदायक प्रतीत होते हैं, क्योंकि कुफ़्र सर्वप्रथम उसकी अभिरुचि और उसके स्वभाव ही पर आक्रमण करके उसे विकृत कर देता है। फिर उसकी दशा उस रोगी जैसी हो जाती है जिसके रोग ने उसकी ज़बान का मज़ा ख़राब कर दिया हो और उसे मीठी चीज़ कड़ुवी लगती हो। क़ुरआन में है—
“अतः क्या वह व्यक्ति जिसके लिए उसका बुरा कर्म शोभायमान बना दिया गया हो, और वह उसे अच्छा समझ रहा हो ...... अतः अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है।" (क़ुरआन, 35:8)
सबसे बड़ी गुमराही और अज्ञानता यही है कि आदमी की अभिरुचि और उसका स्वभाव ही विकृत हो जाए और वह सुरुचि और सुन्दर भावों के आनन्द से वंचित होकर रह जाए।
नैतिकता का सम्बन्ध मानव-जीवन से
(1) हज़रत नवास-बिन-समआन (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से नेकी और गुनाह के विषय में पूछा। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जवाब दिया—
“नेकी सुशीलता है और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे और तुम्हें यह अप्रिय हो कि लोग उसे जान जाएँ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि नेकी अपनी वास्तविकता की दृष्टि से सुशीलता से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। सुशीलता ही का दूसरा नाम नेकी है। जिसका जीवन सुशीलता से रिक्त है, वह नेकी के समस्त गुणों से वंचित है। जिस चीज़ को आदमी स्वभावतः न चाहे, जिससे वह सन्तुष्ट न हो, जो हृदय में चुभे, जिसे वह स्वयं भी अप्रिय समझता हो और उसे यह भी पसन्द न हो कि दूसरे लोग उसे जान लें, वही गुनाह है। इसके विपरीत जो चीज़ हमारे स्वभावानुकूल हो, जो हमारे स्वभाव को प्रिय हो, जिसे व्यावहार में लाने से, हृदय को प्रसन्नता प्राप्त होती हो, वही नेकी है।
नेकी और गुनाह एक-दूसरे के विपरीत हैं। जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकार दोनों का एकत्र होना सम्भव नहीं, उसी प्रकार नेकी (सुशीलता) और गुनाह को कभी एकत्र नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गुनाह का मार्ग अपनाता है, वह सबसे पहले स्वयं अपने प्रति बेवफ़ाई की नीति अपनाता है। गुनाह वस्तुतः विश्वासघात है जो आदमी अपनी प्रकृति और अन्तरात्मा के साथ करता है, जबकि नेकी वास्तव में आत्मज्ञान, स्वाभिमान और चेतनता का दूसरा नाम है।
(2) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा कि ईमान क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जवाब दिया—
“जब अच्छा काम करके तुम्हें प्रसन्नता हो और बुरा काम करके अप्रसन्नता तो तुम मोमिन हो।"
उसने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! फिर गुनाह क्या है? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब कोई चीज़ तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे तो उसे छोड़ दो।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : जिस प्रकार ईमान का नैतिकता से गहरा सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार नैतिकता हमारे सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध है और उसे प्रभावित करती है। ईमान पर आधारित नैतिकता से जिस जीवन का आविर्भाव होता है, उसमें नेकियाँ मात्र नेकियाँ नहीं होतीं, बल्कि वे आदमी के जीवन में सबसे बढ़कर प्रसन्नता और निश्चिन्तता का कारण भी होती हैं। इसी प्रकार जीवन में बुराई अत्यन्त अप्रिय चीज़ होती है। यदि इनसानी कमज़ोरी के कारण किसी मोमिन से कोई ख़ता और बुराई हो भी जाती है तो उसकी अन्तरात्मा उसे झिंझोड़ कर रख देती है। उसकी सारी ख़ुशी छिन जाती है। जब तक वह अपनी ग़लती सुधार नहीं लेता, उसे चैन और सन्तोष प्राप्त नहीं होता।
(3) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह का डर रखो जहाँ कहीं भी हो, और बुराई के बाद नेकी कर लो, ताकि नेकी बुराई को मिटा दे और लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार सुशीलता का हो।” (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)
व्याख्या : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हदीस है। आदमी जहाँ कहीं और जिस हालत में भी हो, धनी हो या निर्धन, ताक़तवर हो या कमज़ोर, रात के अन्धकार और एकान्त में हो या दिन के प्रकाश में और लोगों की निगाहों के सामने हो, उसे अल्लाह की बड़ाई और महानता का सदैव लिहाज़ करना चाहिए। यही चीज़ उसे अत्याचार, सरकशी, अपमान या अधमता और प्रत्येक प्रकार के गुनाहों से सुरक्षित रखेगी और यही चीज़ उसे अल्लाह से भी निकट कर देगी, यहाँ तक कि वह अल्लाह का अत्यन्त प्रिय बन्दा बन सकता है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अगर दुर्भाग्य से आदमी से कोई बुराई हो भी जाए तो अल्लाह की दया से वह निराश न हो, तुरन्त उसके सुधार की चिन्ता करे।"
इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार (अल्लाह से क्षमा याचना) करने के साथ-साथ कोई अच्छा काम भी करे, जिससे उस गुनाह और बुराई के दुष्प्रभाव उसके मन-मस्तिष्क से दूर हो जाएँ और उसके गुनाह की गन्दगी बाक़ी न रहे। यह चीज़ ईश्वरीय अनुकम्पा को आकृष्ट करने में उसके लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी।
फिर जिस प्रकार अल्लाह का यह विशेष हक़ है कि यह बन्दा हर स्थान पर और हर समय अपने ईश्वर को याद रखे और उसकी तरफ़ से ग़ाफिल न हो। उसी प्रकार ईश्वर के बन्दों का भी ईश्वर पर यह हक़ है कि उनके साथ उसका जो मामला भी हो वह नैतिकता पर आधारित हो। जनसामान्य का भी हमपर हक़ है और वे हमारे लिए इसकी कसौटी भी हैं कि हम किस तरह के मनुष्य हैं— स्वार्थी, अहंकारी और गिरे हुए या विशालहृदय, उच्च और सच्चरित्र।
नैतिकता का व्यापक गुण
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने तुम्हारी नैतिकता को तुम्हारे मध्य उसी प्रकार वितरित किया है, जिस प्रकार उसने तुम्हारी आजीविका को तुम्हारे बीच वितरित किया है। अल्लाह दुनिया तो उसको भी देता है जिससे प्रेम करता है और उसको भी देता है जिससे प्रेम नहीं करता। मगर 'दीन' केवल उसी को प्रदान करता है जिससे उसे प्रेम होता है। अतः जिस व्यक्ति को अल्लाह ने 'दीन' प्रदान किया है अनिवार्यतः उससे उसको प्रेम है। उस सत्ता की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! कोई बन्दा उस समय तक मुस्लिम नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी ज़बान मुस्लिम न हो। और वह उस समय तक मोमिन नहीं होता जब तक कि उसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से सुरक्षित न हो।" (हदीस : मुस्नद अहमद, बेहक़ी)
व्याख्या : नैतिकता के अध्ययन के सिलसिले में यह एक महत्वपूर्ण हदीस है। सांसारिक जीवन में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली आजीविका या धन आदि जिसकी ओर सामान्यतः लोगों का झुकाव होता है और इसे प्राप्त करने में वे बेपरवाही से काम नहीं लेते। धन के द्वारा आदमी अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता या अपनी ज़िन्दगी की सुख-सुविधा में बढ़ोत्तरी करता है। दूसरी चीज़ वह है जिसे नैतिक गुण कहते हैं। नैतिकता का वास्तविक सम्बन्ध आदमी के अपने आप से और व्यक्तित्व से होता है। आदमी कैसा है? यह उसकी दौलत से नहीं उसके नैतिक व्यवहार से मालूम कर सकते हैं। आदमी नैतिकता की दृष्टि से यदि अच्छा नहीं है तो धन की प्रचुरता से यह कमी पूरी नहीं हो सकती। इसकी मिसाल बिलकुल ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति जीर्ण-शीर्ण और सदा बीमार रहनेवाला हो और उसकी बीमारी भी ऐसी हो कि जिसके कारण वह निरन्तर कष्ट और पीड़ा में ग्रस्त हो तो उसके धनवान होने के बावजूद उसका जीवन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी कोई कामना करे। नैतिकता की ख़राबी शारीरिक बीमारी से कहीं अधिक चिन्ताजनक होती है। यह लोगों का दृष्टिदोष ही है कि वे नैतिक गुणों के मूल्य और महत्व को सामान्यतः महसूस नहीं करते।
धन-दौलत का अल्लाह की दृष्टि में कोई बड़ा महत्व नहीं है। यही कारण है कि अल्लाह अपने दुश्मनों तक को दौलत दे देता है, लेकिन नैतिक गुण केवल अपने उन्हीं बन्दों को प्रदान करता है जिनसे उसे प्रेम होता है। अल्लाह किस व्यक्ति से प्रेम करता है इसकी पहचान इससे होती है कि किस व्यक्ति को उसकी ओर से नैतिक गुणों की निधि प्रदान की गई है।
इस हदीस में स्वयं नैतिकता को ही दीन (धर्म) ठहराया गया है। अतएव “जिस व्यक्ति को अल्लाह ने दीन (धर्म) प्रदान किया है" वाक्य में 'दीन' शब्द 'नैतिकता' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। नैतिकता को 'दीन' ठहराने से वास्तविक उद्देश्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि इनसान अपने नैतिक स्तर को ऊँचा करे। जीवन में धर्म का वास्तविक आधार वस्तुतः नैतिक चेतना ही है। अल्लाह की बन्दगी और उसका आज्ञापालन और धर्म के समस्त आदेशों का पालन ही वास्तव में हमारी नैतिकता है। 'दीने-हक़' (सत्य-धर्म) से पलायन चाहे वह किसी भी रूप में हो, वस्तुतः एक गम्भीर नैतिक अपराध है।
(2) हज़रत अम्र-बिन-अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में हाज़िर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस मामले (धर्म) में आपके साथ (इस्लामी आमन्त्रण के आरम्भ में) कौन था? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“एक आज़ाद और एक ग़ुलाम।"
मैंने कहा कि इस्लाम क्या है? आप (सल्ल) ने कहा—
“पवित्र और उत्तम बोल और खाना खिलाना।"
मैंने कहा कि ईमान क्या है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “धैर्य और उदारता।" उल्लेखकर्ता कहते हैं कि मैंने कहा कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन-सा है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उस व्यक्ति का जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें।"
उल्लेखकर्ता कहते हैं कि मैंने कहा कि सबसे अच्छा ईमान कौन-सा है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छी नैतिकता।"
वे कहते हैं कि मैंने कहा कौन-सी नमाज़ सबसे अच्छी है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“(नमाज़ में) दास्यभाव से देर तक खड़े रहना।” उल्लेखकर्ता कहते हैं कि मैंने कहा कि कौन-सी हिजरत सबसे अच्छी है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यह कि जो कुछ तेरे रब को अप्रिय हो उसे तू छोड़ दे।” उल्लेखकर्ता कहते हैं कि इसके पश्चात् मैंने पूछा कि कौन-सा जिहाद अच्छा है?
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"उस व्यक्ति का जिसका घोड़ा मारा जाए और जिसका अपना भी ख़ून बहाया जाए।" उल्लेखकर्ता कहते हैं कि मैंने कहा—
“घड़ियों में कौन-सी घड़ी सबसे अच्छी है?"
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मध्य रात्रि का अन्तिम भाग।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : हजरत अबू-बक्र-सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत ज़ैद-बिन-हारिसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें सबसे पहले ईमान लाने का श्रेय प्राप्त हुआ है।
इस्लाम केवल कल्पना की दुनिया में सीमित होकर रहना नहीं चाहता, बल्कि उसे अपेक्षित यह है कि जीवन के विभिन्न मामलों में उसकी अच्छे से अच्छे अन्दाज़ में अभिव्यक्ति हो। उदाहरणस्वरूप, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यहाँ दो बातों का उल्लेख किया, जो सामान्य और विशिष्ट सभी लोगों के जीवन में पेश आती रहती हैं।
इससे यह भी मालूम हुआ कि इस्लाम सर्वथा भलाई और दिलों को निहाल कर देने का दूसरा नाम है। मधुर वाणी, अच्छी वार्ता और उदारता एवं दानशीलता (खाना खिलाना जिसका एक स्पष्ट प्रमाण है) केवल वाणी की सुन्दरता और केवल कर्म की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि यह चीज़ स्वयं आदमी की अपनी गुणवत्ता और उसकी प्रियता का भी प्रमाण है। आदमी अगर लोकप्रिय न भी हो तो इस गुण को अपना लेने के पश्चात् बहुत जल्द लोगों के दिलों में उसके लिए जगह पैदा हो जाएगी और वह लोकप्रिय बन कर रहेगा। यह गुण ऐसा है कि जिससे स्वयं इसके अपनानेवाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी आनन्ददायक परिवर्तन आएगा और उसके व्यक्तित्व में लोगों के लिए विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा।
ईमान वास्तव में परोक्ष और पारलौकिक तथ्यों पर विश्वास करने का नाम है। इसके विपरीत ग़ैर-ईमानी हालत यह है कि आदमी की दृष्टि मात्र प्रत्यक्ष पर हो। ऐसा आदमी भौतिक रूप से शीघ्र प्राप्त होनेवाले फ़ायदे ही को सब कुछ समझ लेता है और इसे प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित प्रत्येक उपाय करता है। जाइज़ और नाजाइज़, या वर्जित और अवर्जित की उसे कोई परवाह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में रुपये ख़र्च कर सकता है जिसमें उसे सांसारिक लाभ की अधिक आशा हो, लेकिन किसी मुहताज की सहायता या भलाई और कल्याण के काम में रुपये ख़र्च करना उसके लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। जबकि ईमान आदमी को इस संकीर्णता और तंगी से निकाल लेता है। ईमान आदमी को दूरदर्शी और विशाल-हृदय बनाता है। धैर्य और सब्र इसी दूरदर्शिता, दानशीलता, उदारता और विशाल-हृदयता का प्रतीक है। धैर्य इस बात का प्रमाण है कि आदमी की दृष्टि ऐसी चीज़ पर है जो सामान्य दृष्टियों से ओझल है और दानशीलता और उदारता इस बात का पता देती है कि आदमी की रूह (अन्तरात्मा) लोभ-लालच और कृपणता के बन्धन से मुक्त हो चुकी है।
एक मोमिन व्यक्ति को कोई कष्ट और तकलीफ़ पहुँचे या वह आर्थिक तंगी और किसी प्रकार के कष्टों और परेशानियों से दो-चार हो तो वह समझता है कि सब कुछ उसके रब की निगाहों में है। वहीं सबसे अच्छा सहायक और रक्षक है। उसे अपने रब की कारसाज़ी पर पूरा भरोसा होता है। वह कहता है कि हमें तो उस फ़र्ज़ की अदाएगी में अपनी ऊर्जा और अपने समय का सर्वश्रेष्ठ भाग लगाना चाहिए, जिसे अल्लाह ने हमारे लिए नियत किया है। रही समस्याएँ और उलझनें, तो उनसे निबटने के लिए हमारा रब काफ़ी है। इसलिए उन सभी कष्टप्रद स्थितियों में, जिनमें सामान्य रूप से लोग धैर्य खो देते हैं बल्कि कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, ईमानवाला व्यक्ति अत्यन्त धैर्य एवं दृढ़ता का सुबूत देता है, और यह केवल उसकी ईमान की शक्ति का चमत्कार होता है।
एक दूसरे पहलू से इस्लाम का यह प्रभाव प्रकट होना चाहिए कि एक मुसलमान से उसके किसी भाई को किसी प्रकार की आशंका और कोई हानि का भय शेष न रहे। यदि किसी मुसलमान के जीवन में इस्लाम का यह भाव प्रकट नहीं होता तो समझ लीजिए कि वह अभी तक इस्लाम के उत्तम स्वरूप से अनभिज्ञ है।
मूल-पाठ में 'तूलुल-क़ुनूत' का शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ नमाज़ में खड़े होने की लम्बी अवधि के अतिरिक्त क़ुरआन का अधिक से अधिक पाठ और ईश्वर के प्रति अधिक से अधिक विनयशीलता भी लिया गया है। 'क़ुनूत' वास्तव में नमाज़ की मूल आत्मा है। नमाज़ में यह चीज़ जितनी अधिक पाई जाएगी, उतना ही अधिक उसे श्रेष्ठ माना जाएगा।
सामान्य अर्थ में हिजरत अल्लाह की ख़ुशी और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपना देश और घर-बार छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाने को कहते हैं। देश और देशवासी किसको प्रिय नहीं होते, लेकिन हिजरत करनेवाला इन सबके मुक़ाबले में अल्लाह की ख़ुशी और प्रसन्नता को प्राथमिकता देता है। अपनी ख़ुशी और पसन्द के मुक़ाबले में अल्लाह की ख़ुशी और उसकी पसन्द को अपनाना, यही हिजरत की मूल आत्मा है, जिसका क्रियान्वयन घर-बार छोड़ने ही में नहीं बल्कि जीवन के समस्त मामलों में अपेक्षित है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन से मालूम हुआ कि हमारे रब को जो नापसन्द हो उसे हम छोड़ दें तो यह एक अच्छी क़िस्म की हिजरत है, यद्यपि इस हिजरत में स्थानान्तरण न पाया जाता हो। उस रुचि और रुझान और उस कार्य को छोड़ देना जो अल्लाह को पसन्द न हो, देश और स्थान के त्याग से कहीं बड़ा और क्रान्तिकारी त्याग है। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ हिजरत की संज्ञा देना अत्यन्त अर्थपूर्ण है।
फ़िदा होने का यह अन्दाज़ कितना भाव-विभोर कर देनेवाला है कि जिहाद के मैदान में न केवल यह कि वह स्वयं क़ुरबान हो गया, बल्कि उसका घोड़ा भी लौटकर घर न आया। इसे सबसे अच्छे जिहाद से निरूपित करना इस्लाम के सच्चे होने का खुला प्रमाण है, क्योंकि इस्लाम का मौलिक गुण यह है कि वह इनसान को वह दृष्टि प्रदान करता है जिसके कारण सांसारिक और भौतिक लाभ-हानि के आवरण सामने से हट जाते हैं और आदमी को यह दिखाई देने लगता है कि उसके लिए वास्तविक लाभ की बात क्या है और वास्तविक हानि उसके लिए किस चीज़ में है।
मध्यरात्रि का अन्तिम भाग रात का वह भाग है जो अत्यन्त शान्तिमय और आत्मा को उन्नत करनेवाला होता है। इनसान के अन्तःकरण पर उस समय नमाज़ में खड़े होने, अल्लाह के समक्ष झुकने और सजदा करने से अत्यन्त गहरे प्रभाव पड़ते हैं। जो तनहाई और एकाग्रता रात की इस घड़ी में प्राप्त होती है, वह किसी दूसरी घड़ी में प्राप्त नहीं होती। दास्यभाव से परिपूर्ण हृदयों के लिए तो यह घड़ी एक बड़ी नेमत है। यह वह विशेष समय है जो ईश्वर की वन्दना और उसके समक्ष अपनी असमर्थता और ईश्वर के प्रति दास्यभाव के प्रकट करने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है, क्योंकि उस समय दुआ के क़बूल होने और बन्दे की ओर उसके रब की रहमतों के उन्मुख होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यह वह समय होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है, जिसके कारण दिखावे में ग्रस्त होने की आशंका कम ही होती है।
(3)
आदर्श नैतिकता
(दृष्टि एवं विवेक)
शुद्धहृदयता
(1) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“सारे कर्म नीयत पर निर्भर करते हैं। अतः जिस किसी की हिजरत दुनिया प्राप्त करने या किसी स्त्री से विवाह करने के लिए होगी, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने घर-बार छोड़ा। और जिस किसी व्यक्ति ने अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए हिजरत की होगी, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए है।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : बुख़ारी ही की एक रिवायत में ये शब्द आए हैं—
"सारे कर्म बस नीयत पर ही निर्भर करते हैं।"
इनमें भावार्थ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है।
यह एक महत्त्वपूर्ण हदीस है जिसमें एक अत्यन्त बुनियादी बात स्पष्ट शब्दों में बयान की गई है। इसकी महत्ता को देखते हुए इमाम बुख़ारी ने 'सहीह बुख़ारी' के आरम्भ में इस हदीस को रखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को सात स्थानों पर उद्धृत किया है, जिससे इस हदीस की महत्ता और उपयोगिता का भली-भाँति अन्दाज़ा होता है। इस हदीस की एक विशेषता यह भी है कि इसे तीन ताबई— यह्या, मुहम्मद और अलक़मा एक-दूसरे से नक़ल करते हैं।
इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) का कथन है कि यह हदीस इस्लाम का एक तिहाई है। अर्थात् इस्लामी शिक्षाओं के एक तिहाई हिस्से को इस हदीस ने अपनी परिधि में ले रखा है। कुछ दूसरे बुज़ुर्गों ने इसे इस्लाम का एक चौथाई हिस्सा ठहराया है। इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) की दृष्टि में इस हदीस का सम्बन्ध फ़िक़्ह (धर्मशास्त्र) के सत्तर सर्गों (अबवाब) से है। यह इस हदीस की संग्राहकता का स्पष्ट प्रमाण है।
ग़लत इरादे से या बेहोशी या बेख़बरी की हालत में आदमी जो कुछ करता है उससे उसकी उन्नति और तरक्क़ी नहीं होती। नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है कि सारे कर्म सजगतापूर्वक किए जाएँ। आदमी यदि बड़ी और ऊँची चीज़ों के मुक़ाबले में छोटी और तुच्छ चीज़ों को अपना उद्देश्य ठहराकर जीवन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह कभी भी उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। और इस परिस्थिति का वह स्वयं उत्तरदायी होता है। उच्चता की प्राप्ति तो उसके अपने निर्णय और इरादे पर निर्भर करती है। इनसान के किसी कर्म के पीछे अगर मूल प्रेरक-तत्व अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आज्ञापालन है, तो निश्चय ही यह उच्चता की ओर उसकी एक पेशक़दमी है। जीवन के उच्च उद्देश्य उसकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेशों और वचनों ही से हमें अपनी भलाई और सफलता और अपने कल्याण का ज्ञान प्राप्त होता है। अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आज्ञापालन से न केवल यह कि हमारा जीवन, जीवन के उच्च आशय और उद्देश्यों से समरसता प्राप्त कर लेता है, बल्कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन भी अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आज्ञापालन ही है।
यह हदीस हमें सचेत करती है कि हम अपनी नीतियों एवं कार्यों में सदैव अपने इरादों और नीयतों का जाइज़ा लेते रहें, जिससे किसी समय भी हमारा जीवन सत्य से विलग न रह सके।
(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने प्रतापवान रब के सम्बन्ध में कहते हैं—
“अल्लाह ने नेकियाँ और बुराइयाँ लिख दी हैं, फिर उसे स्पष्ट भी कर दिया है। अतः जिस व्यक्ति ने किसी नेकी का इरादा किया और उसे किया नहीं तो अल्लाह उसके लिए अपने पास एक पूरी नेकी लिख देता है। और यदि उसने इरादा करके उसे कर भी लिया तो अल्लाह उसके लिए अपने पास दस नेकियों से लेकर सात सौ गुना तक बल्कि उससे भी ज़्यादा लिख देता है। इसके विपरीत जिस किसी व्यक्ति ने किसी बुराई का इरादा किया लेकिन वह बुराई उसने की नहीं तो अल्लाह उसके लिए भी अपने पास पूरी एक नेकी लिखता है, और यदि वह बुराई और गुनाह कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए केवल एक बुराई लिखता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नेकी क्या है? बुराई किसे कहते हैं? यह कोई पहेली नहीं। अल्लाह के यहाँ यह चीज़ अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं है। जिन चीज़ों को शाश्वत मूल्यों से समरसता प्राप्त है, वास्तव में वही नेकियाँ हैं। बुराई वह है जिसका स्थायी एवं उच्च मूल्यों से कोई सम्बन्ध न हो। यह अल्लाह की रहमत है कि उसने सविस्तार बता भी दिया है कि कौन-से कर्म शाश्वत और उच्च मूल्यों से सम्बन्ध रखते हैं और कौन-से ऐसे कर्म हैं जो शाश्वत और सर्वव्यापी मूल्यों के प्रतिकूल हैं।
यह हदीस बताती है कि अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब (प्रकोप) से बढ़ी हुई है। क़ुरआन में भी है—
“कहा: अपनी यातना में तो मैं उसी को ग्रस्त करता हूँ जिसे चाहता हूँ, किन्तु मेरी दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है।" (7:156)
अल्लाह के यहाँ ज़ुल्म और बेइनसाफ़ी नहीं पाई जाती। वह दानशील और उदार है। हाँ यह अवश्य है कि उसकी दानशीलता और उदारता अन्धे की बाँट नहीं है। नेकी तो नेकी ही है चाहे वह देखने में कितनी ही छोटी और साधारण क्यों न हो, अल्लाह उसे अकारथ नहीं करता। वह नेकी भी आदमी के किसी न किसी चरित्र और नैतिकता की प्रतीक होती है।
(3) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा—
“ऐ अल्लाह, इसे हिक्मत (तत्वदर्शिता और समझ-बूझ) प्रदान कर।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : हिक्मत क्या है? इस विषय में बुज़ुर्गों और पहले के लोगों के विभिन्न कथन मिलते हैं, जो वस्तुतः हिक्मत ही के किसी न किसी पहलू को स्पष्ट करते हैं। अपनी मूल प्रकृति की दृष्टि से हिक्मत एक ऐसा प्रकाश, विवेक और ऐसी मनोदशा है जिससे सुन्दरता और असुन्दरता या भलाई और बुराई दोनों ही पहलू उजागर हो जाते हैं। हिक्मत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे साधारण वस्तुओं की तरह अर्जित किया जाए। यह विवेक और तत्वदर्शिता सर्वथा दैवयोग से प्राप्त होती है। यह वास्तव में एक प्रकार का इलहामी ज्ञान है। यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति किसी स्वादिष्ट चीज़ को चखे और उसके स्वाद को अपनी सूक्षम-इन्द्रियों से पहचाने और उसका पूर्णतया रसास्वादन करे। मालिक और अबू-रज़ीन के कथन से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कहते हैं कि हिक्मत धर्म में गहरी समझ और उस अन्तःप्रज्ञा का नाम है जिसको परितोष और दिव्य-प्रकाश कहा जा सकता है। यह हिक्मत जब आदमी के कथनों, कर्मों और उसके वैचारिक और ज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र में भी प्रकट होती है तो इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे : नसीहत, उपदेश, कृतज्ञता, दानशीलता, न्याय, सहनशीलता और पवित्रता आदि। उदाहरणार्थ क़ुरआन में है—
“और हमने लुक़मान को हिक्मत प्रदान की थी कि ईश्वर का कृतज्ञ हो।" (31:12)
इस सूरा में आगे इस कृतज्ञताप्रकाशन और हिक्मत के अन्तर्गत एकेश्वरवाद, आख़िरत पर ईमान, नमाज़, नेक कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना, मुसीबतों में धैर्य से काम लेना, घमंड और लोगों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाने से बचना, चाल और रफ़्तार में मध्यमार्ग का अनुसरण और बातचीत में मृदुलता— इन दस बातों का उल्लेख किया गया है। इनमें से दो का सम्बन्ध धारणा से है, शेष आठ बातों में से चार संकल्प और इरादे और मुसीबतों में धैर्य और दृढ़ता से काम लेने से सम्बन्धित हैं और शेष चार का सम्बन्ध नैतिकता से है।
वस्तुतः कृतज्ञता ईमान की आधारशिला है और हिक्मत का विशेष प्रदर्शन भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिक्मत पूरी ज़िन्दगी पर प्रभावी है। क़ुरआन के इस कथन से वास्तविकता सामने आ जाती है—
“और जिसे हिक्मत दी गई, उसे तो बड़ी दौलत मिल गई।" (2 : 269)
इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती।
(4) हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से ईश्वरीय मार्ग में युद्ध के बारे में पूछा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी क्रोधावस्था में लड़ता है और जातीय पक्षपात के कारण (या अज्ञान में पक्षपात के कारण) युद्ध करता है।” उल्लेखकर्ता कहते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सिर उठाया, क्योंकि वह व्यक्ति खड़ा था (और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैठे हुए थे), फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "जो व्यक्ति इसलिए लड़े कि अल्लाह का बोल ऊँचा रहे तो वह युद्ध अल्लाह की राह में है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : नीयत के ठीक रखने और धर्म के प्रति निष्ठा के महत्व के अतिरिक्त यह हदीस इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम में युद्ध या लड़ाई का उद्देश्य कितना पवित्र और उच्च है। व्यक्तिगत द्वेष और शत्रुता और क़ौमी जज़्बे या अज्ञानपूर्ण पक्षपात जैसी चीज़ों का इस्लाम में युद्ध के लिए कोई औचित्य नहीं है। इस्लाम में युद्ध का मूल उद्देश्य अल्लाह का बोलबाला करना और न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना है। जिस युद्ध से फ़ितना और फ़साद पैदा हो उसकी इस्लाम कदापि अनुमति नहीं देता।
(5) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो कोई अल्लाह से मिलने को पसन्द करता है, तो अल्लाह भी उससे मिलने को पसन्द करता है। और जो व्यक्ति अल्लाह से मिलने को नापसन्द करता है, तो अल्लाह भी उससे मिलने को नापसन्द करता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मोमिन की हार्दिक इच्छा अपने रब से मिलने ही की होती है। यही इच्छा उसके हृदय को जीवन्त और उसे प्रत्येक प्रकार के अन्धकार से दूर रखती है। जो व्यक्ति अल्लाह से मिलने का इच्छुक हो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने हृदय में किसी ऐसी चीज़ को स्थान देगा जो घृणित हो। पसन्द और नापसन्द का सम्बन्ध वस्तुतः आदमी के अपने हृदय से होता है। यदि अल्लाह से मिलने की चाह उसके अन्दर नहीं पाई जाती, तो अल्लाह के विषय में तो यह बात स्पष्ट है कि वह निरपेक्ष है, उसे क्या पड़ी है कि वह ऐसे ना-क़दरे की क़द्रदानी करे।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“क़ियामत के दिन सबसे पहले जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाएगा, यह वह व्यक्ति होगा जो शहीद हो गया था। उसे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो अल्लाह उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह उनको स्वीकार करेगा।" अल्लाह कहेगा, "तूने इन नेमतों से क्या काम लिया” वह कहेगा कि मैंने तेरे लिए युद्ध किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा, “तू झूठा है, बल्कि सत्य यह है कि यह युद्ध तूने इसलिए किया कि लोग तुझे वीर कहें। तो तुझे वीर कहा जा चुका।" फिर अल्लाह के आदेशानुसार उसे मुँह के बल घसीटते हुए ले जाकर नरक में डाल दिया जाएगा।
और एक वह व्यक्ति होगा जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों को उसकी शिक्षा दी और क़ुरआन पढ़ा। वह अल्लाह के समक्ष पेश किया जाएगा तो अल्लाह उसे भी अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह उनको स्वीकार करेगा। अल्लाह कहेगा, “तूने इन नेमतों से क्या काम लिया?" वह कहेगा कि मैंने इल्म हासिल किया और दूसरों को भी उसकी शिक्षा दी और तेरे लिए क़ुरआन पढ़ा। अल्लाह कहेगा, “तू झूठा है, तूने तो इल्म इसलिए हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कहें। और क़ुरआन तूने इसलिए पढ़ा कि लोग तुझे क़ारी कहें। तो तुझे यह सब कहा जा चुका।" फिर अल्लाह के आदेशानुसार उसे मुँह के बल घसीटते हुए ले जाकर नरक में डाल दिया जाएगा। फिर एक वह व्यक्ति होगा जिसे अल्लाह ने कुशादगी दी थी और उसे हर प्रकार का माल दे रखा था। उसे अल्लाह के समक्ष पेश किया जाएगा तो अल्लाह उसे भी अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह उनको स्वीकार करेगा। फिर अल्लाह कहेगा, “तूने इन नेमतों से क्या काम लिया?" वह कहेगा कि मैंने कोई ऐसा मार्ग, जिसमें ख़र्च करना तुझे प्रिय था, नहीं छोड़ा कि उसमें तेरे लिए ख़र्च न किया हो। अल्लाह कहेगा, "तू झूठा है, बल्कि सत्य यह है कि तूने केवल इसलिए ख़र्च किया कि लोग तुझे दानशील कहें। तो यह उपाधि तुझे मिल चुकी।" फिर अल्लाह के आदेशानुसार उसे मुँह के बल घसीटते हुए ले जाकर नरक में डाल दिया जाएगा। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से स्पष्ट होता है कि जीवन का बड़े से बड़ा कारनामा या कार्य भी अल्लाह की दृष्टि में तुच्छ है, जब तक कि उसके पीछे अल्लाह की ख़ुशी हासिल करने की इच्छा कार्यरत न हो। अल्लाह अपने बन्दों से प्रेम करता है, जबकि बन्दे भी अल्लाह से प्रेम करें। आदमी वहीं होता है जहाँ उसकी नीयत या इरादा होता है। वास्तव में आदमी अपनी नीयत में छिपा होता है। उसकी पहचान उसकी नीयत ही से हो सकती है। नीयत अगर ईश्वरीय प्रसन्नता से इतर कुछ और है तो यह एक ऐसा घोर अपराध है जो बन्दे को न केवल यह कि स्वर्ग से वंचित कर देता है बल्कि उसे नरक का पात्र भी बना देता है। नीयत यदि ठीक नहीं है तो इस स्थिति में आदमी देखने में नेक अमल कर रहा होता है, किन्तु तथ्यात्मक दृष्टि में वह एक अक्षम्य अपराध कर रहा होता है।
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिसने ऐसे ज्ञान को जिससे ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है उसे लौकिक स्वार्थ के लिए सीखा तो क़ियामत के दिन उसे स्वर्ग की सुगन्ध भी न मिल सकेगी।" (हदीस : अबू-दाऊद)
“एक और हदीस है। हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ और कहा कि एक व्यक्ति इसलिए लड़ता है कि उसका नाम लिया जाए, एक इसलिए लड़ता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, एक इसलिए लड़ता है कि माले-ग़नीमत (युद्ध स्थल से प्राप्त शत्रु-धन) उसके हाथ आए और एक व्यक्ति इसलिए लड़ता है कि उसका दर्जा ऊँचा हो (अर्थात् बहादुरी में उसे उच्च स्थान प्राप्त हो)। इस पर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जो व्यक्ति इसलिए लड़ता है कि ईश्वर का बोल-बाला हो, उसी की लड़ाई प्रतापवान ईश्वर के मार्ग में समझी जाएगी।।” (हदीस : अबू-दाऊद)
(7) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति सच्चे दिल से शहीद होने का इच्छुक हो उसे शहीद होने का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, चाहे उसके शहीद होने की नौबत न आए।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इसी प्रकार एक और हदीस है—
“जो व्यक्ति सच्चे दिल से शहीद होने की इच्छा करता है तो अल्लाह उसे शहादत की मंज़िलों तक पहुँचा देता है, यद्यपि उसकी मृत्यु उसके अपने बिस्तर पर ही क्यों न हुई हो।" (हदीस : मुस्लिम)
इन हदीसों से मालूम हुआ कि धर्म में नीयत की दुरुस्ती मौलिक रूप से अभीष्ट है। कर्मों को नीयत के बाद देखा जाता है। किसी विवशता के कारण यदि कोई व्यक्ति कर्म करने में असमर्थ रहा तो इससे अल्लाह के प्रति उसकी निष्ठा और वफ़ादारी में कोई कमी नहीं होती। बन्दा यदि अल्लाह के लिए अपने को आत्यान्तिक रूप से पेश कर देना चाहता है तो वह सफल है। बन्दा यदि अल्लाह के दीन के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देने को तैयार है तो वह अल्लाह के प्रति निष्ठावान है, चाहे व्यावहारिक रूप में इसकी नौबत न आए।
(8) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि हम एक लड़ाई में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम जब भी चलते हो या कोई घाटी पार करते हो, वे तुम्हारे साथ होते हैं। रोग ने उन्हें वहाँ रोक लिया है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात अल्लाह के मार्ग में निकलने का उन्हें भी सवाब मिलेगा, क्योंकि विवशता के कारण उन्हें घर पर रुकना पड़ा। वे कोई जान चुरानेवाले लोग नहीं हैं। उनकी गणना अल्लाह के यहाँ दीन की सेवा करनेवाले लोगों ही में होगी, क्योंकि यद्यपि वे अपने हाथ-पैर से काम न ले सके लेकिन दिल से वे प्रत्येक सेवा के लिए तैयार रहे।
(9) हज़रत सलमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
"अल्लाह के मार्ग में एक रात और एक दिन पहरा देना महीना भर रोज़ा रखने और नमाज़ पढ़ने से श्रेष्ठ है। मरने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति का यह कर्म बराबर जारी रहेगा, उसकी जीविका भी जारी हो जाएगी और वह क़ब्र के फ़ितने से निश्चिन्त होगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इनसान के कर्मों का सिलसिला उसकी मृत्यु के साथ टूट जाता है। एक अन्य हदीस से भी पता चलता है कि सदक़ा-जारिया (अर्थात जिससे लोगों को निरन्तर फ़ायदा पहुँचता रहे), लाभदायक ज्ञान और नेक औलाद के अलावा आदमी के अन्य कर्मों का सिलसिला मृत्यु के पश्चात् टूट जाता है। लेकिन यह हदीस बताती है कि इस्लामी सीमा आदि की सुरक्षा और निगरानी का काम भी इतना महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम भी इतने दूरगामी हैं कि मृत्यु के पश्चात् भी इसका अज्र और सवाब उसी प्रकार मिलता रहेगा जिस प्रकार जीवन में करने के समय मिलता है। ऐसा व्यक्ति उस विशिष्ट जीविका का भी अधिकारी हो जाता है जो शहीदों के लिए नियत है। साथ ही क़ब्र की मन्ज़िल भी उसके लिए आसान कर दी जाती है।
(10) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह तुम्हारे रूप-रंग और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि उसकी नज़र तुम्हारे दिलों और तुम्हारे कर्मों पर होती है।" (हदीम : मुस्लिम)
व्याख्या : कुछ हदीसों में ये शब्द मिलते हैं—
“अल्लाह तुम्हारे शरीरों, तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे कर्मों को नहीं देखता, बल्कि मूलतः वह तुम्हारे दिलों को देखता है।" (हदीस : जमउल-फ़वाइद, भाग-2)
दिलों को देखने का मतलब यह है कि अल्लाह की नज़र वास्तव में इस पर होती है कि तुम्हारे मनोभावों और तुम्हारी मनोवृत्तियों की दशा क्या है। तुम्हारे अन्दर निष्ठा और अल्लाह के प्रति समर्पण का भाव है या नहीं। ईमान के भाव से तुम्हारे दिल परिपूर्ण हो सके हैं या नहीं। दिल में अगर ईमान के स्थान पर कुफ़्र, पवित्रता और निष्ठा के स्थान पर अनिष्ठा और अपवित्र भावनाएं पाई जाती हैं, तो अच्छे चेहरों और बाह्य कर्मों की अल्लाह की नज़र में कोई क़ीमत बाक़ी नहीं रहती।
(11) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह कहता है कि मैं सभी साझीदारों के शिर्क से बेपरवाह हूँ कि किसी को अपना शरीक बनाऊँ। जिसने कोई ऐसा कर्म किया जिसमें उसने मेरे साथ दूसरे को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शिर्क दोनों को छोड़ देता हूँ।"
और एक रिवायत में है—
“मेरा उस कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, वह उसी के लिए है। जिसको उसने कर्म में मेरे साथ शरीक किया।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : दीन में अपेक्षित केवल इतना ही नहीं है कि हमारे कर्म अल्लाह के लिए हों, बल्कि अपेक्षित यह है कि हमारे कर्म अल्लाह ही के लिए हों। किसी और की प्रसन्नता प्राप्त करना हमारे समक्ष न हो। यदि हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं तो वे कभी भी अल्लाह के यहाँ स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह स्वाभिमानी है, वह शिर्क को कदापि नहीं सहन कर सकता।
एक हदीस में है—
"जिस किसी ने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी, उसने शिर्क किया और जिस किसी ने दिखावे के लिए रोज़ा रखा, उसने शिर्क किया और जिस किसी ने दिखावे के लिए सदक़ा किया, उसने शिर्क किया।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
(12) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क़ियामत कब आएगी? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अफ़सोस है तुझपर, उसके लिए क्या तैयारी की है?" उसने कहा, मैंने तैयारी तो कोई नहीं की है, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता हूँ।" रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे प्रेम है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि उन्होंने इस्लाम के पश्चात् मुसलमानों को किसी चीज़ से इतना प्रसन्न होते नहीं देखा, जितना नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से वे प्रसन्न हुए।
व्याख्या : हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि क़ियामत कब आएगी? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि “तूने उसके लिए क्या तैयारी की है?” उसने कहा कि नमाज़, रोज़े आदि की अधिकता तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम करता हूँ। इस पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह प्रेम करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
निष्ठा की मूल आत्मा प्रेम ही है। प्रेम ही है जो आदमी को किसी के लिए प्रत्येक पहलू से एकाग्रचित कर देता है। कहा गया है—
अजब चीज़ है लज्ज़ते-आश्नाई।
प्रेम निष्ठा की मूल आत्मा है। इसलिए बन्दे को जीवन और उसके परलोक के सिलसिले में निर्णायक स्थान प्राप्त है। यहीं से यह भी मालूम हुआ कि दीन की मूल आत्मा और अभिप्राय भी ईश-प्रेम ही है। अतएव इमाम इब्ने-तैमिया (रहमतुल्लाह अलैह) ने कहा है कि अल्लाह का प्रेम ही मूल धर्म है। इसी प्रेम की पूर्णता पर धर्म की पूर्णता निर्भर करती है। इस प्रेम में किसी प्रकार की कमी धर्म में कमी का पर्याय है। (देखिए फ़तावा शैख़ुल इस्लाम अहमद इब्ने-तैमिया (रहमतुल्लाह अलैह), खंड-10, पृष्ठ-57)
सहाबा के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कहना कि "तू उसी के साथ होगा जिससे तू प्रेम रखता है" एक ख़ुशख़बरी थी। वे अपने कर्मों की ओर से सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे कि इस सिलसिले में उनसे कोई कोताही न होगी। किन्तु वे देख रहे थे कि उनके हृदय अल्लाह और उसके रसूल के प्रेम से परिपूर्ण हैं। अल्लाह और रसूल का प्रेम उनके जीवन की सबसे बहुमूल्य निधि बन चुका था, इसलिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से यह सुनकर कि मनुष्य उसी के साथ होगा जिससे उसे प्रेम है, उन्हें विश्वास हो गया कि ईश्वर उन्हें अपने समीप और अपने रसूल के संग-साथ से वंचित न करेगा। आदमी के हक़ में वास्तविक निर्णायक चीज़ वह प्रेम है जो वह किसी के साथ रखता है।
(13) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति अपने बिस्तर पर इस नीयत से लेटा कि वह तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठेगा, लेकिन उसकी नींद उसपर ऐसी छा गई कि वह सुबह को ही उठ सका, तो जिस चीज़ की उसने नीयत की वह उसके कर्म-पत्र में लिख दी जाएगी और उसकी नींद उसके अपने रब की ओर से उसके लिए एक सद्क़ा और पारितोषिक है।" (हदीस : नसई, इब्ने-माजा)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि अपनी नीयत के कारण उसे तहज्जुद (रात्रि के अन्तिम पहर की नमाज़) का सवाब मिल गया। वह रात में नर्म बिस्तर पर विश्राम करता रहा, किन्तु सत्य की दृष्टि में वह जागा हुआ ही रहा। यह विश्राम उसके गौरवमय अल्लाह का एक अनुग्रह और पारितोषिक हुआ।
इनसान की नीयत और उसका संकल्प ही मौलिक चीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन लोग अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे।" (हदीस : इब्ने-माजा)
अर्थात् जैसी उनकी नीयतें होंगी, उन्हीं के लिहाज़ से वे अच्छे या बुरे परिणाम से दो चार होंगे।
(14) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने लोगों का माल ऋण के रूप में इस इरादे से लिया कि उसे अदा कर देगा और किसी मजबूरी के कारण अदा न कर सका तो अल्लाह उसकी ओर से अदा कर देगा। और जिस किसी ने ऋण लिया लेकिन उसकी नीयत उसे अदा करने की नहीं है तो अल्लाह उसकी इस बदनीयती के कारण उसे विनष्ट करके रहेगा।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात् नीयत अगर ठीक है तो ऋण अदा न होने पर भी अल्लाह के यहाँ वह अपराधी नहीं ठहरेगा। वह ऋण भी अल्लाह उसकी ओर से चुका देगा, लेकिन यदि उसकी नीयत ठीक नहीं है तो नीयत की ख़राबी उसे ले डूबेगी, वह बरबाद होने से कदापि न बच सकेगा। अल्लाह हम सभी को नीयत की ख़राबी और ग़लत रुझानों और झुकावों से बचाए रखे। आमीन!
वास्तविक अपराध या गुनाह नीयत की ख़राबी है। बुद्धिसंगत विवशता (उज़्र) अल्लाह के यहाँ स्वीकार्य है। अतएव हदीस में है—
“जब आदमी अपने किसी भाई से कोई वादा करे और उसकी यह नीयत हो कि वह उस वादे को पूरा करेगा, लेकिन किसी कारणवश वह उसको पूरा न कर सके और वह वादे पर न आए तो उसपर कोई गुनाह नहीं।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
अल्लाह आदमी की नीयत और उसकी विवशताओं से भली-भाँति परिचित है। बेबस और असमर्थ की गिरफ़्त करना उसकी दया और न्याय की शान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इन स्पष्ट व्याख्याओं के पश्चात भी क्या इस्लाम के सत्य और स्वाभाविक-धर्म होने में कोई सन्देह किया जा सकता है?
(15) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने प्रेम किया तो अल्लाह के लिए, द्वेष रखा तो अल्लाह के लिए, दिया तो अल्लाह के लिए, और अपना हाथ रोका तो अल्लाह ही के लिए, तो निश्चय ही उसने अपने ईमान को पूर्णत्व तक पहुँचा दिया।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : प्रेम, द्वेष, देना और न देना इसी का नाम जीवन है। मानव-जीवन में ये सभी चीज़ें पेश आती हैं। ईमान और पूर्ण ईमान की बात यह है कि यह सब कुछ किसी और भावना के अन्तर्गत नहीं बल्कि केवल ईश्वर की प्रसन्नता और उसके मुखारविन्द की चाह के लिए हो। ईमान की दृष्टि से पूर्ण व्यक्ति वही है जो प्रेम उसी से करता है, जिससे प्रेम का सम्बन्ध रखना अल्लाह को प्रिय है। जिस व्यक्ति से अल्लाह विरक्त है, उससे वह भी विरक्त होगा। वह ख़र्च वहाँ करेगा जहाँ अल्लाह ने ख़र्च करने का हुक्म दिया है। वहाँ उसका हाथ रुक जाएगा जहाँ ख़र्च करना अल्लाह को प्रिय नहीं है।
ज्ञान
(1) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
"जो कोई ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से राह चले तो अल्लाह उसके कारण उसे जन्नत की एक राह चलाता है। फ़रिश्ते ज्ञान चाहनेवाले की प्रसन्नता के लिए अपने पर बिछाते हैं और निश्चय ही ज्ञानवान के लिए वे सब जो आकाशों और धरती में हैं, क्षमायाचना करते हैं, यहाँ तक कि वे मछलियाँ भी जो पानी में होती हैं। उपासना करनेवाले पर ज्ञानवान को ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त है जैसे चौदहवीं रात के चन्द्रमा को समस्त तारों पर श्रेष्ठता प्राप्त है। निस्सन्देह ज्ञानवान लोग ही पैग़म्बरों के उत्तराधिकारी हैं। पैग़म्बरों ने किसी को दीनार और दिरहम का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने केवल ज्ञान की मीरास छोड़ी। अतः जिस किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, उसी ने ही पूरा हिस्सा प्राप्त किया।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में ये शब्द भी आए हैं—
“ज्ञानवान (आलिम) को उपासक पर ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त है, जैसी श्रेष्ठता मुझे तुममें से साधारण व्यक्ति के मुक़ाबले में प्राप्त है।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
इस हदीस से भली-भाँति अन्दाज़ा किया जा सकता है कि इस्लाम में ज्ञान का क्या स्थान है। धर्म का ज्ञान ही वह धन है जिसे लेकर सारे ही नबी दुनिया में आए और अपने पीछे वे इसी को मीरास की शक्ल में छोड़ गए। इससे जो लाभान्वित न हुआ, उससे बढ़कर अभावग्रस्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जिस किसी ने इस मीरास को प्राप्त कर लिया, उसके हिस्से में प्रचुर धन आ गया। उसने प्रचुरता को न्यूनता के मुक़ाबले में और प्रतिष्ठित को अप्रतिष्ठित के मुक़ाबले में प्राथमिकता प्रदान की।
ज्ञानवान व्यक्ति लोगों को प्रिय होता है। उसकी लोकप्रियता दुनिया में छिपी नहीं रह सकती, बल्कि फ़रिश्तों को भी ऐसे व्यक्ति से अत्यन्त प्रेम होता है
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त करने की चाहत में राह चलता है। तो इसके कारण अल्लाह अनिवार्यतः उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सुगम कर देता है। और जिसका साथ देने में उसके कर्म ने विलम्ब किया तो उसके साथ उसकी कुलीनता तीव्रगामी नहीं हो सकती।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ज्ञान की इच्छा अपने परिणाम की दृष्टि से जन्नत की इच्छा है और ज्ञान-प्राप्ति अपनी वास्तविकता की दृष्टि से जन्नत की प्राप्ति है। ज्ञान के अभाव में आदमी उस मार्ग से बेख़बर ही रहता है जो जन्नत की ओर जाता है। ज्ञान के बिना किसी कर्म और विशेष रूप से ऐसे कर्म की आशा नहीं की जा सकती जिसके पीछे समयक विवेक, चेतना और उत्तम प्रकार के मनोभाव पाए जा सकें। ज्ञान से वंचित व्यक्ति के चरित्र और कर्म कदापि ऐसे नहीं हो सकते जो धर्म में अभीष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही कुलीन और प्रतिष्ठित वंश से सम्बन्ध रखता हो, उसके जीवन में जो अभाव रह जाता है उसकी पूर्ति उसकी कुलीनता से सम्भव नहीं है।
(3) हज़रत मुआविया-बिन-अबी-सुफ़ियान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति के साथ अल्लाह भलाई चाहता है, उसे धर्म में समझ प्रदान करता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : किसी को यदि धर्म में समझ-बूझ प्राप्त है तो यह इस बात का लक्षण है कि ईश्वर के समक्ष उसके लिए भलाई और कल्याण है। वह असफल और घाटा उठानेवाला न होगा। यदि धर्म में समझ-बूझ प्राप्त न हो तो आदमी धर्म की अपेक्षाओं को समझने में असमर्थ रहता है। उससे इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह 'दीन' की अपेक्षाओं को सही अन्दाज़ में पूरा करेगा। दीन में समझ प्राप्त होने के पश्चात् ही हम किसी से यह आशा कर सकते हैं कि वह दीन की अपेक्षाओं की अनदेखी नहीं करेगा और नादानी में कोई ऐसी नीति नहीं अपनाएगा जो दीन या उसके अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से घातक और विनाशकारी हो। अतएव एक हदीस में आया है—
“जान लो! उस इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें समझ नहीं है। उस ज्ञान में कोई भलाई नहीं जिसमें कोई समझ-बूझ नहीं है। उस क़ुरआन-पाठ में कोई भलाई नहीं। जसमें सोच-विचार और चिन्तन नहीं।”
इसी प्रकार एक और हदीस में है—
“लोगों में सबसे अच्छे वे लोग हैं जो कर्म की दृष्टि से उनमें सबसे अच्छे हैं, जबकि वे अपने 'दीन' (धर्म) में समझ-बूझ रखते हों।"
कौन व्यक्ति समझ-बूझ रखनेवाला है, इस सिलसिले में हदीस में एक मिसाल बयान हुई है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी व्यक्ति का नमाज़ को दीर्घ करना और अपने ख़ुत्बे (अभिभाषण) को संक्षिप्त करना, उसके समझदार होने का लक्षण है।” (हदीस : मुस्लिम)
नमाज़ और ख़ुतबे ही में नहीं दूसरे मामलों में भी समझ-बूझ रखनेवाले और न रखनेवाले में आप अन्तर पाएँगे। समझदार व्यक्ति का ध्यान मूल उद्देश्य की ओर से नहीं हट सकता, जबकि नासमझ व्यक्ति दूसरी चीज़ों की ओर अधिक आकृष्ट दिखाई देता है। इस सिलसिले में एक अच्छी मिसाल इस हदीस में पेश की गई है—
“नासमझ लम्बे-चौड़े ख़ुतबे देगा, यहाँ तक कि वह नमाज़ को संक्षिप्त कर देगा, किन्तु ख़ुतबे को संक्षिप्त नहीं कर सकता, जबकि समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ख़ुतबा नसीहत है और नमाज़ अपने आप में इबादत है। जिस किसी ने नमाज़ को संक्षिप्त किया और ख़ुतबा लम्बा दिया वह समझदार नहीं, क्योंकि वह ख़ुतबे में शरीअत की पाबन्दी और इबादत पर लोगों को उभारता है और स्वयं अपने कर्म से उसका खंडन करता है। वह इस तरह कि नमाज़ जैसी इबादत को संक्षिप्त कर देता है। कर्म के प्रति उदासीनता ज्ञान के अपूर्ण और दोषयुक्त होने का प्रमाण है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो कर्म में परिलक्षित हो।”
(4) हज़रत अब्दुल्लाह-इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“एक व्यक्ति नमाज़ और रोज़े का पाबन्द, ज़कात अदा करनेवाला, हज और उमरा करनेवाला होता है —यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तमाम नेकियों का उल्लेख किया— किन्तु क़ियामत के दिन उसे उसकी बुद्धि के अनुसार ही बदला और प्रतिदान मिलेगा।” (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हदीस है। यह हदीस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस्लाम धर्म सहज-स्वाभाविक धर्म है। इसके सारे प्रावधान और मूल्य सहज स्वभाव के बिलकुल अनुरूप हैं। धर्म में यदि बुद्धि और समझ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तो यही इसका कारण है। बाह्य कर्मों के पीछे आदमी की कैसी भावनाएँ और प्रेरक शक्तियाँ काम करती हैं, यह अधिकतर उसकी बुद्धि और समझ पर निर्भर करता है। हमारे कर्मों का वास्तविक मूल्य हमारी भावनाएँ और अनुभूतियाँ ही नियत करती हैं। अतः बदला और प्रतिदान प्रदान करने में मौलिक रूप से बुद्धि और विवेक को दृष्टि में रखना न्याय और प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है।
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब लोगों को हुक्म देते तो उन्हीं कर्मों (को अपनाने) का हुक्म देते जिनके करने की उनमें शक्ति होती। सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! हम आप जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने तो आपके अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। इसपर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सख़्त ख़फ़ा हुए, यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चेहरे से नाराज़गी प्रकट होने लगी। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं तुम सबसे अधिक अल्लाह का डर रखनेवाला और अल्लाह को जाननेवाला हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक हदीस में है—
“ख़ुदा की क़सम! मैं सबसे अधिक अल्लाह को जानता हूँ और सबसे बढ़कर उसका डर रखता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
इस हदीस से मालूम हुआ कि धर्म में मूलतः यह अपेक्षित नहीं है कि लोग अनावश्यक रूप से अपने आपको मशक़्क़तों और परेशानियों में डाल लें, जबकि वास्तविकता यह है कि यह धर्म आया ही इसलिए है कि उन बन्धनों को काट दे जिनमें लोग जकड़े हुए हों और उनपर से वह बोझ उतारे जिससे उनकी कमरें झुकी जा रही हों। अल्लाह का 'दीन' (धर्म) तो लोगों को कठिनाइयों में डालने के बजाए उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आया है। इसी लिए इस 'दीन' (धर्म) की विशेषता बताई गई है कि “निश्चय ही यह 'दीन' (धर्म) आसान है" एक हदीस में है— "तुम्हारा उत्तम दीन वह है जो आसान हो।”
कठिनाइयों और अपने आपको यातना में ग्रस्त करना धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म वह चीज़ है जो हमारे जीवन में सम्मिलित होकर हमारा जीवन बन सके। हमारी प्रकृति के प्रतिकूल कोई चीज़ कभी भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तित्व का आवश्यक अंश नहीं बन सकती। धर्म वही है जो जीवन बन सके, न कि जीवन के लिए बोझ।
एक अन्य तथ्य जो इस हदीस से ज्ञात होता है वह यह है कि धर्म का मूल आधार ईश-ज्ञान है। इसी पर धर्म का सम्पूर्ण भवन निर्मित होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अल्लाह को जानता और पहचानता होगा, उतना ही अधिक उसका जीवन धर्म के साँचे में ढल सकेगा। क़ुरआन में है—
“अल्लाह से तो उसके बन्दों में वही लोग डरते हैं जो जानने और समझने वाले हैं।"
ईश-ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि आदमी ईश्वरीय सत्ता के यथार्थ को पा ले, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि आदमी को अल्लाह की सत्ता, उसकी महानता और बड़ाई का पूरा यक़ीन हो जाए। उसे यह आभास होने लगे कि इस सृष्टि में एक महान सत्ता की क्रियाशीलता स्पष्टतः पाई जाती है। वह बाह्य जगत् और अन्तर में फैली हुई ईश्वर की निशानियों की ओर से ग़ाफ़िल और अन्धा बनकर न रहे। वह ईश्वर के गुण और उसके स्वभाव से अपरिचित न रहे। धर्म से सम्पर्क वास्तव में अल्लाह से सम्पर्क ही का दूसरा नाम है। धर्म अल्लाह की इच्छा और उसकी मंशा के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति अल्लाह को पहचानता है, उसे उसकी महानता का भी एहसास होगा। फिर यह कैसे सम्भव है कि वह धार्मिक रास्ते से हटे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन से अभिप्रेत यह है कि 'जब मैं तुम सबसे अधिक अल्लाह को जानता हूँ और तुम सबसे अधिक उससे डरता हूँ, तो फिर मेरे लिए यह कैसे सम्भव है कि मैं धर्म के अपेक्षित और वांछित तरीक़े की उपेक्षा कर सकूँ। तुम्हारे लिए मेरा तरीक़ा ही अनुकरणीय है।'
(6) हज़रत अब्दुल्लाह-इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईर्ष्या केवल दो आदमियों के मध्य जाइज़ है— एक तो वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने माल दिया, फिर उसे सत्यमार्ग में लुटाने की सामर्थ्य प्रदान की। और दूसरा वह व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने हिक्मत (तत्त्वदर्शिता) प्रदान की, तो वह उसके अनुसार फ़ैसले करता और (लोगों को) उसकी शिक्षा प्रदान करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : ईर्ष्या से यहाँ अभिप्रेत स्पर्धा से है। आशय यह है कि उल्लिखित दोनों विशेषताओं को अपने अन्दर पैदा करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए।
इस हदीस से यह मालूम होता है कि वही दो व्यक्ति जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है ऐसे हैं जिनका जीवन इतना सफल है कि उनके मुक़ाबले में किसी को सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। जीवन में कोई व्यक्ति अपने लिए सुख-सुविधा का कितना ही सामान जुटा ले, किन्तु वास्तव में उनका कोई महत्व नहीं है। किसी का कथन है—
"इस दुनिया में हम जो कुछ लेते हैं वह नहीं, बल्कि जो कुछ देते हैं, वह हमें धनवान बनाता है।"
इन दो विशेषताओं के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है और कोई विशेषता नहीं जिसको महत्व दिया जा सके। अतः इनके अतिरिक्त किसी और चीज़ के प्रति स्पर्धा या ईर्ष्या हमारी संकीर्णता और ओछेपन ही का प्रतीक हो सकती है। ईर्ष्या तो अनैतिक चीज़ है। यदि ईर्ष्या जाइज़ होती तो दुनिया में दो ही विशेषताएँ ऐसी हैं, जिनपर कोई ईर्ष्या कर सकता था, जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है। यह बात बिलकुल ऐसी ही है जैसे कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यदि मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने पति को सजदा करे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
(7) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब इनसान मर जाता है तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग हैं— जारी रहनेवाला सदक़ा, या ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : जारी रहनेवाले सदक़े की मिसाल में औक़ाफ़, मस्जिद का निर्माण, कुआँ खुदवाना आदि सम्मिलित हैं। किसी को शिक्षा दी या कोई लाभप्रद पुस्तक लिखी कि मृत्यु के पश्चात् भी उस पुस्तक से लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे, जारी रहनेवाले सदक़े की एक मिसाल यह भी है।
(8) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन का पेट भलाई (ज्ञान और तत्वदर्शिता की बातों) से कभी नहीं भरता। वह उसे सुनता रहता है, यहाँ तक कि अन्ततः वह जन्नत में पहुँच जाता है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ज्ञान वही है जिसका सम्बन्ध इनसान की भलाई और कल्याण से किसी न किसी रूप में हो। नेकी की बातों को सुनने से मोमिन कभी नहीं अघाता। वह तो ऐसी बातों को सुनने और जानने का लोभी होता है। जिस प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति सांसारिक सुख-सुविधा का लोभी होता है, चाहे उसके पास कितनी ही अधिक दौलत सिमटकर आ जाए, लेकिन वह दौलत से उकताता नहीं है, ठीक इसी प्रकार मोमिन ज्ञान और तत्वदर्शिता का भूखा होता है। वह ज्ञान से लाभान्वित होता रहता है। यह चीज़ उसकी शान्ति और निश्चिन्तता का कारण भी होती है और व्यावहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन भी। ऐसा व्यक्ति सत्यमार्ग पर क़ायम रहता है, यहाँ तक कि वह जन्नत में पहुँच जाता है, जहाँ उसके लिए पूर्ण शान्ति और आनन्द का सामान मौजूद होता है।
(9) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तुम जानते हो कि सबसे बढ़कर दानशील कौन है?" सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भली-भाँति जानते हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अल्लाह सबसे बढ़कर दानशील है, फिर आदम की सन्तान में सबसे बढ़कर मैं दानशील हूँ। और मेरे बाद लोगों में सबसे बढ़कर दानशील वह होगा जिसने इल्म हासिल किया, फिर उसे फैलाया। वह क़ियामत के दिन एक नायक के रूप में आएगा।" या आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि “इस हैसियत से आएगा कि वह अपने आप में एक पूरा समुदाय होगा।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : दानशीलता एक सराहनीय मौलिक गुण है। दानशीलता समस्त नैतिक गुणों की मूल आत्मा है। दानशीलता वास्तव में जीवन का लक्षण बल्कि स्वयं जीवन है। मृत व्यक्ति से कोई आशा नहीं की जा सकती। वृक्ष उसी समय तक छाया और फल देता है, जब तक वह जीवित है। सूख जाने के पश्चात् उससे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अल्लाह चूँकि जीवन का मूल स्रोत है, इसलिए उसकी दानशीलता और अनुकम्पा का भी कोई अन्त नहीं है। इस आधारभूत गुण 'दानशीलता' में जो जितना अधिक बढ़ा हुआ होगा, अल्लाह से भी वह उतना ही अधिक निकट होगा। नबी को अल्लाह से अधिक सामीप्य प्राप्त होता है जो किसी दूसरे को नहीं होता। इसलिए दानशीलता में वह सबसे बढ़ा हुआ होता है।
इस हदीस से ज्ञान के प्रचार-प्रसार की महत्ता का भली-भाँति अन्दाज़ा किया जा सकता है। ज्ञान का प्रसार चाहे वह किसी रूप में हो उसका सम्बन्ध नुबूवत के मूल कर्तव्य से होता है। अतः इसकी महत्ता में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं। नबी यूँ तो हर दृष्टि से दानशील होता है, लेकिन उसकी असल दानशीलता उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार है जो अल्लाह की ओर से उसे प्रदान होता है। फिर उसके प्रचार-प्रसार में वह हर प्रकार के कष्ट और तकलीफ़ें सहन करता है।
यह दानशीलता की पराकाष्ठा है कि जिन लोगों की ओर से कष्ट और तकलीफ़ पहुँच रही हो, जो लोग उसके आगे मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर रहे हों, वह उन्हें ज्ञान और विवेक की दौलत से मालामाल कर देने और उनकी ज़िन्दगियों को सँवारने के लिए प्रयासरत हो।
फिर दुनिया में उस व्यक्ति ने जिस प्रकार का काम किया उसकी अपेक्षा यह थी कि वह अकेले एक बड़े गरोह पर भारी हो। जिसकी हैसियत क़ौम के नायक की हो उसकी महानता का क्या कहना!
(10) हज़रत यज़ीद-बिन-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपसे बहुत-सी बातें सुनी हैं। मुझे भय है कि उसका आरम्भ और अन्त मुझे याद न रहे इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझे ऐसी बात बतला दें जो संग्राहक हो। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जो कुछ जानते हो उसके विषय में अल्लाह से डरते रहो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन की पृष्ठभूमि बताती है कि यह एक संग्राहक वाक्य है जो बहुत-सी बातों और नसीहतों को अपने में समेटे हुए है। जिस व्यक्ति ने इसे समझकर अपना लिया, उसके लिए भलाई और कल्याण के सभी मार्ग खुल जाएँगे।
"जो कुछ जानते हो उसके विषय में अल्लाह से डरते रहो" में कई बातों की ओर संकेत मिलता है। इससे एक बात तो यह मालूम हुई कि जब तक अल्लाह का डर और लिहाज़ न हो सुधार के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ यह भी आवश्यक है कि आदमी अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करे। यह ज्ञान का सुदृढ़ आधार भी है। फिर कर्म के प्रेरकों में सबसे बढ़कर प्रेरक अल्लाह का डर ही है। जहाँ अल्लाह का डर न पाया जाता हो, वहाँ देखने में चाहे ज्ञान और विवेक का कितना ही बड़ा भंडार क्यों न संचित हो गया हो, यह नहीं कहा जा सकता कि आदमी अपने जीवन में ज्ञान का आदर भी करेगा। नैतिक विषयों से सम्बन्धित कुछ किताबों में यह उल्लेख मिलता है कि नीतिशास्त्र के अध्ययन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि इससे आदमी अनिवार्यतः नैतिकता का पालन भी करेगा। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से यह भी मालूम हुआ कि ईमानवाले व्यक्ति के पास जो कुछ भी ज्ञान है, यदि वह उसका हक़ पहचानता है और उसे जीवन में अपना मार्गदर्शक बनाता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि यदि उसका ज्ञान और अधिक होता तो वह उसका भी अपने जीवन में लिहाज़ रखता। वास्तव में भरोसा उसके इसी भाव और सत्यनिष्ठा का किया जा सकता है। हर ईमानवाले के पास इतना ज्ञान होता ही है जो मुक्ति के लिए पर्याप्त है। शर्त यह है कि वह उस ज्ञान को अपनी अकर्मण्यता से नष्ट न करे।
रज़ीन की एक हदीस में “इत्तक़िल्ला-ह फ़ीमा तअ्लम" (जो कुछ जानते हो उसके विषय में अल्लाह से डरते रहो) के अतिरिक्त “वअ्मल बिहि" (इस पर अमल करो) के शब्द भी आए हैं, जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह से डरने का तक़ाज़ा है कि आदमी जो कुछ जानता है उसपर अमल भी करे।
(11) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अबुल-क़ासिम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उस सत्ता की क़सम जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं! जो कुछ मैं जानता हूँ, यदि तुम जानते तो रोते अधिक और हँसते कम।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अबुल-क़ासिम से अभिप्रेत नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के एक पुत्र का नाम क़ासिम था इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अबुल-क़ासिम (अर्थात क़ासिम के पिता) कहा जाता था।
आदमी की पोज़ीशन दुनिया में इतनी अधिक नाज़ुक है कि भविष्य में जो कुछ होनेवाला है, उसका ज्ञान और एहसास यदि पूरी तरह उसे हो जाए तो जीवन की घड़ियों में उसके पास हँसने के लिए कम और रोने के लिए अधिक समय होगा। अल्लाह की महानता और उसके प्रताप का ख़याल कभी भी उसे बेपरवाह होने नहीं देगा। आदमी को हँसी सामान्यतः बेपरवाही की हालत में आती है।
एक हदीस में है कि अर्श की छाया में स्थान पानेवालों में वह व्यक्ति भी होगा जिसने तन्हाई की हालत में अल्लाह को याद किया और उसकी आँखें आँसुओं से छलक गईं। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
(12) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की एक दुआ यह थी—
‘‘ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उस ज्ञान से जो लाभप्रद न हो और उस दुआ से जो सुनी न जा सके और उस हृदय से जो विनीत न हो सके और उस जी से जो कभी न अघाए।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : आदमी के लिए यह परिस्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है कि लाभदायक ज्ञान से वंचित हो, उसकी दुआ न सुनी जाए और उसके हृदय में विनयशीलता न हो और धन से उसका जी कभी न भरे। यह मनोदशा अत्यन्त गम्भीर है। इसलिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इन सभी से सुरक्षित रहने की पनाह माँगी है। हिदायत पानेवाला व्यक्ति तो वह होता है जिसका ज्ञान लाभप्रद हो, अल्लाह उससे राज़ी हो और उसकी पुकार सुनी जाती हो, उसका दिल विनम्रता से परिपूर्ण हो और मन सन्तुष्ट हो। उसकी दशा उस भूखे जानवर जैसी न हो जो प्रत्येक हरे चारे पर मुँह मारता फिरता हो और फिर भी अघाता न हो। ऐसा व्यक्ति हिदायत और मार्गदर्शन से दूर होता है। यह आशा करना कि ऐसा व्यक्ति सत्यमार्ग पर आएगा, कठिन है।
इन चारों चीज़ों पर अलग-अलग विचार कीजिए जिनसे बचने के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने रब से पनाह माँगी है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस ज्ञान से, जो लाभप्रद न हो, पनाह माँगी है। वह ज्ञान लाभप्रद नहीं है जिससे न ईमान को ताज़गी प्राप्त होती हो और न वह आदमी के सांसारिक जीवन के लिए कारआमद हो। ऐसा सत्यज्ञान भी जिससे आदमी न ख़ुद फ़ायदा उठाए और न दूसरों को उसके द्वारा फ़ायदा पहुँचाए, अलाभकारी ज्ञान के अन्तर्गत आता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। क़ुरआन और सुन्नत के अध्ययन से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि ही न करें, बल्कि हमारा प्रयास यह हो कि वह ज्ञान लाभप्रद सिद्ध हो। वह ज्ञान हमारे जीवन में उतर आए। कर्म के बिना ज्ञान सही अर्थ में नहीं होता। आदमी धर्म की बहुत-सी बातें जानता है और जानने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में उसने बस वही जाना जितना उसने अपने जीवन में अपनाया। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में वह ज्ञान विश्वसनीय नहीं जो कर्मरहित हो। इसके साथ ही हमारी यह कोशिश भी हो कि हमारे ज्ञान से अल्लाह के दूसरे बन्दों को भी फ़ायदा पहुँचे, और फ़ायदा पहुँचने के इस दायरे का विस्तार होता चला जाए। हमारे ज्ञान से ईमानवालों को भी फ़ायदा पहुँचे और वह उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बन सके जो ईमान की दौलत से वंचित हैं।
दूसरी चीज़ जिससे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पनाह माँगते थे वह अस्वीकृत प्रार्थना है। वह दुआ स्वीकार नहीं होती जिसके पीछे सत्यनिष्ठा न हो। आदमी हराम एवं अवैध कमाई से अपना पेट भरने में लगा हो, उसके शरीर पर अवैध कमाई का परिधान हो और हलाल रोज़ी की उसे कोई चिन्ता न हो। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही गिड़गिड़ाकार दुआएँ माँगे, अल्लाह उसकी दुआओं को कैसे सुन सकता है? जो व्यक्ति अल्लाह से कोई सम्बन्ध न रखे, जीवन में अल्लाह के मुक़ाबले में द्रोहपूर्ण नीति अपनाए, अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी पसन्द की उपेक्षा करे, वह आख़िर अल्लाह को किस मुँह से आवाज़ देता और उसे पुकारता है? अल्लाह की दृष्टि में उसकी दुआ का क्या महत्व हो सकता है? हदीस से यह भी मालूम होता है कि जब बुराइयाँ आम हो जाएँ, यहाँ तक कि बुराइयाँ फैलाई जाने लगें और भलाइयों का मार्ग रोका जाने लगे तो अल्लाह उस समय दुआ सुनने से इनकार कर देता है और ऐसी मुसीबतों और कठिनाइयों में लोगों को डाल देता है कि बड़े-बड़े मामलों की परख रखनेवाले लोग भी चकित होकर रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि इससे छुटकारे के लिए क्या किया जाए।
तीसरी चीज़, जिससे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पनाह माँगी है, वह ऐसा दिल है जो विनम्रता से ख़ाली हो। जिस दिल में विनम्रता न हो वह दिल अचेत और मृतप्राय है। मृत हृदय किसी काम का नहीं होता। वह बंजर भूमि के सदृश होता है जो कृषि योग्य नहीं होती। विनयशीलता की वास्तविकता क्या है? विनयशीलता, जिसके लिए मूल हदीस में “ख़ुशूअ्” शब्द प्रयुक्त हुआ है, का अर्थ होता है— सुकून, विनयप्रदर्शन, और नम्रता। वह दीवार जो गिरकर ज़मीन से आ लगती है— उसे "जिदारुन ख़ाशिउन” कहते हैं। “मकानुन ख़ाशिउन" उस स्थान को कहते हैं जिसका रास्ता न मिल सके। इसी प्रकार "बलदतुन ख़ाशिअतुन" उस नगर को कहते हैं जिसमें ठहरने का कोई स्थान न हो। पत्ते के मुरझा जाने, धरती के सूख जाने और आवाज़ के मद्धम पड़ जाने को भी इसी शब्द से अभिव्यंजित किया जाता है। इस प्रकार क़ल्बे-ख़ाशेअ् (दिल की विनम्रता) की वास्तविकता यह समझ में आती है कि इससे अभिप्रेत वह दिल है जिसके अन्दर विनम्रता और विनयशीलता हो, वह अल्लाह के आगे झुका हो और उसके समक्ष नत हो। अल्लाह की महानता के एहसास से वह पिघला हुआ हो, अल्लाह के सिवा ग़ैर के उसके अन्दर प्रविष्ट होने की गुंजाइश बाक़ी न हो, वह अल्लाह की महानता के समक्ष नत और दूसरे के ख़याल से बिलकुल मुक्त हो और हर पहलू से अल्लाह के लिए एकाग्र हो चुका हो। विनम्रता का पूर्ण प्रदर्शन नमाज़ में होता है, जबकि बन्दा हर तरफ़ से अल्लाह के लिए एकाग्र हो जाता है तथा पूरी निश्चिन्तता के साथ अल्लाह के आगे सर्वथा विनम्र और विनयशील बन जाता है। अल्लाह से कुछ पाने और दीन और ईमान की अनुकम्पाओं से परिपूर्ण होने के लिए विनम्रता उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार पानी को बहने के लिए उस दिशा की आवश्यकता पड़ती है जिधर ढलान हो। विनम्रता के अभाव से दिल सख़्त हो जाता है और ख़ुदा से सबसे दूर वह दिल होता है जो सख़्त हो।
चौथी चीज़ जिससे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पनाह माँगी है वह ऐसा जी है जो कभी न अघाए। मन की तृप्ति का सम्बन्ध ईमान से है। ईमान के बिना मन की भूख कभी नहीं मिटती। दुनियापरस्त लोगों को देखिए। उनकी दौलत उन्हें तृप्त करने में असमर्थ है, अपितु उनकी दौलत उनकी भूख को और भी बढ़ा देती है। इस प्रकार वे कभी भी सफल दिखाई नहीं देते। इसके विपरीत ईमानवाले अभाव में भी सन्तुष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज़ प्राप्त होती है जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ भी तुच्छ नज़र आती है।
(13) हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़ज्र की नमाज़ के पश्चात् कहा करते थे—
“ऐ अल्लाह! मैं तुझसे लाभप्रद ज्ञान, स्वीकृत कर्म और पवित्र आजीविका की प्रार्थना करता हूँ।" (हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, बैहक़ी)
व्याख्या : लाभप्रद ज्ञान से अभिप्रेत वह ज्ञान है जो उपयोगी हो, व्यर्थ और निरुद्देश्य न हो। लाभप्रद ज्ञान वही है जिससे ईमान को शक्ति प्राप्त हो, जिससे धर्म की समझ में अभिवृद्धि हो, जिसके कारण सत्यमार्ग पर चलना सुगम हो सके, जिसके द्वारा अपने 'धर्म' की सुरक्षा सम्भव हो, जो स्वप्रतिष्ठा की रक्षा कर सके, जिसके द्वारा सत्यधर्म की सेवा की जा सके और जिसके द्वारा अल्लाह के बन्दों की सेवा का काम भी अंजाम दिया जा सके। इनसान को मन-मस्तिष्क इसलिए नहीं दिया गया कि उसे व्यर्थ से भरा जाए। इनसान का हृदय पालनकर्ता-प्रभु का दृष्टिपटल है। उसे न तो कूड़ा घर बनने देना चाहिए और न स्टोर रूम। यह अत्यन्त अरुचिकर बात है। इससे यह बात भी भली-भाँति समझ में आती है कि जो लोग द्वेष, ईर्ष्या, कपट, लोभ-लालच को अपने अन्दर जगह देते हैं, वे अपने ऊपर अत्याचार करते हैं और नैतिक दृष्टि से आत्यान्तिक पतन का शिकार हो जाते हैं। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि वे चुग़ली, पर-निन्दा, टोह और तोहमत लगाने जैसी नैतिक बीमारियों में ग्रस्त होकर अपना समय नष्ट करते हैं और समाज में बिगाड़ और उपद्रव का कारण बनते हैं।
इस हदीस में वांछित कर्म की परिभाषा यह बताई गई है कि वह स्वीकृत कर्म हो। कर्म के लिए अरबी भाषा में अमल और फ़ेअल दो शब्द आते हैं। यहाँ मूल में 'अमल' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अमल और फ़ेअल, इन दोनों शब्दों में अन्तर पाया जाता है। अमल में संकल्प और इरादा पाया जाता है जबकि फ़ेअल में यह आवश्यक नहीं। अमल निरन्तरता और स्थायित्व चाहता है, क्योंकि वह आदमी की नैतिकता और आचरण को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त अमल सदैव किसी प्रयोजन और उद्देश्य के अन्तर्गत वुजूद में आता है। जो अमल स्वीकृत होगा, वह देखने में भी सभ्य होगा और अपनी मूल आत्मा की दृष्टि से भी पवित्र होगा। स्वीकृत अमल की धारणा हमें हमारे अपने स्रष्टा से जोड़ती है। हमारे सामने अमल का मूल उद्देश्य और प्रयोजन यह होता है कि उसे अल्लाह के दरबार में स्वीकृति प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त हो सके।
भटके हुए लोगों के जीवन की बागडोर उनकी वासनाओं के हाथ में होती है। वे वासना के धक्के खाते फिरते हैं। इसके विपरीत ईमानवाले लोगों का जीवन उनके अपने रब के हुक्म और उसकी प्रसन्नता के अधीन होता है, जिसके कारण उनका जीवन उच्च कोटि का हो जाता है जिसको पवित्र जीवन का नाम दिया गया है। यह अपने प्रकट रूप में पवित्र और आन्तरिक दृष्टि से उत्तम भावनाओं से परिपूर्ण होता है। ईमानवाले लोगों का जीवन ईश-भक्ति का जीवन होता है, जो इनसान के लिए एक उत्कृष्ट निधि है। प्रभु-ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति और उस व्यक्ति के मध्य जो वासनाओं का दास होता है बड़ा अन्तर पाया जाता है। इसे हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। एक तरफ़ वह व्यक्ति है जो गन्दगी का कीड़ा बना हुआ है। गन्दगी में रेंगते रहना ही उसकी नियति है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वभाव की दृष्टि से काव्य और साहित्य से रुचि रखता है। अतः वह साहित्यिक गोष्ठियों की ओर प्रवृत्त होता है। उसका हृदय मृदुल और करुण होता है और उसकी आत्मा ओजपूर्ण और विकल होती है। उसकी कल्पनाएँ और धारणाएँ अत्यन्त उच्च कोटि की होती हैं। ईश-प्रेमी और एक ऐसे व्यक्ति के मध्य जो वासनाओं में ग्रस्त हो जो अन्तर पाया जाता है उसे आप स्वयं समझ सकते हैं।
इबादत और भक्ति-भाव हृदय की एक उच्च मनोदशा और आनन्ददायक उमंग है। यह वह सूक्ष्म चेतना है जिसपर सम्पूर्ण जगत् का सौन्दर्य न्योछावर किया जा सकता है। मोमिन का हर सजदा इस बात का द्योतक होता है कि उसका सम्बन्ध वास्तव में अपने से नहीं बल्कि ईश्वर से होता है। इनसान के लिए यह कोई घाटे की बात नहीं कि ईश्वर जीवनवक्ष में उसका हृदय बन जाए। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की अधिक संख्या दिखाई पड़ती है जो अल्लाह की पसन्द के मुक़ाबले में अपनी सस्ती भावनाओं और वासनाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उन्हें ख़बर नहीं कि उनकी भावनाओं और वासनाओं के मुक़ाबले में कहीं अधिक हमारा ‘अपना' वह है जिसे अल्लाह के नाम से याद किया जाता है।
आजीविका का पवित्र और वैध होना मानव की तीसरी आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि आजीविका हमारी एक आवश्यकता है। आजीविका हमारे शरीर को भी अपेक्षित है और हमारे प्राण को भी। इनसान को जिस आजीविका की इच्छा करनी चाहिए वह पवित्र और वैध आजीविका है। इस हदीस में आजीविका के लिए रिज़्क़ शब्द प्रयुक्त हुआ है। रिज़्क़ अरबी में केवल ख़ुराक ही को नहीं कहते, बल्कि यह प्रदान, बख़्शिश और नसीब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अल्लाह की ओर से जो कुछ हमें मिला है, वह सब हमारा रिज़्क़ है। यहाँ तक कि सन्तान तक रिज़्क में शामिल है। अतएव बहुत-से हदीस के उल्लेखकर्ताओं के नाम 'रिज़्क़', 'रिज़्क़ुल्लाह' और 'रुज़ैक़' मिलते हैं। ज्ञात हुआ कि केवल ख़ुराक ही नहीं, ज्ञान, तत्वदर्शिता, बुद्धिमत्ता, अल्लाह की हिदायत और उसका मार्गदर्शन इत्यादि सभी चीज़ें रिज़्क़ में सम्मिलित हैं।
आदमी को हलाल और पवित्र भोजन से अपने शरीर का पोषण करना चाहिए। ज़ुल्म और ज़्यादती से प्राप्त किया हुआ या छीना हुआ माल खाना चरित्र और नैतिकता की मृत्यु है। जिस प्रकार हमें अपना पेट भरने के लिए आजीविका ही नहीं पवित्र आजीविका चाहिए, ठीक उसी प्रकार मन-मस्तिष्क और हृदय के पोषण के लिए भी पवित्र और विशुद्ध आहार की आवश्यकता है। इस आहार की भी ईश्वर ने पूर्ण व्यवस्था की है। इसके लिए नबियों को भेजा गया। इसी के लिए आसमानी किताबें अवतरित हुईं। ईश्वर का आज्ञापालन और बन्दगी एवं भक्ति भी पवित्र आहार है। नमाज़ आत्मा के लिए उत्तम आहार है। ईश-स्मरण, क़ुरआन पाठ या क़ुरआन का श्रवण आत्मा का मधुमय आहार है। इसी से ईमान में ताज़गी आती है और आत्माएँ विकसित होती हैं। हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) ने जो दुआ सिखाई थी उसका यह पद बहुत प्रसिद्ध है—
“हमारी हर दिन की रोटी हमें हर दिन दे।" (लूक़ा, 11:3)
तात्पर्य यह है कि हमें वह चीज़ प्रदान कर जिससे हमें जीवन मिले। हमें मार्गदर्शन का वह मूलभाव प्रदान कर जो हमें सीधे मार्ग की ओर ले जाए। इसकी पुष्टि हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) के इस कथन से होती है—
“आदमी केवल रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि उस शब्द से जीता है जो ईश्वर की ओर से आता है।"
हमारा प्रत्येक सजदा यह प्रकट करता है कि हम अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं। वह अपने साथ जुड़नेवालों को दूर नहीं रख सकता। इस सम्बन्ध को कर्म और आचरण की शक्ति से सुदृढ़ और मज़बूत बनाने के लिए हमें दुनिया में कर्म क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। जिस प्रकार सजदे से इस सत्य का नवीनीकरण होता है कि हम अल्लाह की ओर पलटनेवाले हैं उसी प्रकार हर अच्छे कर्म द्वारा भी इसी वास्तविकता का प्रदर्शन होता रहता है। एक प्रतीक्षित कल (Tomorrow) की कल्पना जीवन की मूल्यवान निधि है। यही कल्पना हमें कर्म क्षेत्र में गतिशील रख सकती है और हमें ऊँचा उठा सकती है कि हम निःस्वार्थ भाव से अल्लाह के बन्दों को दुनिया और आख़िरत के घाटे से बचा सकें और स्वयं भी हर प्रकार के घाटे से सुरक्षित रह सकें।
समझ और विवेक
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मोमिन एक सुराख़ से दो बार नहीं डसा जाता।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात् मोमिन अनुभव से लाभ उठाता है। यदि वह एक बार किसी सूराख़ से डसा गया तो वह पुनः उसमें हाथ या उँगली नहीं डाल सकता। यदि उसे किसी ने एक बार धोखा दिया तो वह पुनः उस व्यक्ति से धोखा नहीं खा सकता। वह व्यक्ति पुनः उसे हानि नहीं पहुँचा सकता।
यह हदीस बताती है कि ईमान की अपेक्षा यह है कि आदमी बुद्धि और अनुभव से लाभ उठाए तथा अपने को हर प्रकार के धोखे और हानि से बचाए। किसी को एक बार परख लिया तो फिर कभी उसकी चाल और फ़रेब में न फँसे। समझदारी और होशियारी से काम लेना मोमिन का फ़र्ज़ है। जीवन बिताने के लिए जिन बातों का लिहाज़ रखना आवश्यक है, सामान्य लोगों के मुक़ाबले में मोमिन को उनका ख़याल कहीं अधिक रखना चाहिए।
इब्ने-हिशाम ने 'तहज़ीबे-सीरत' में लिखा है कि यह पद कि 'मोमिन एक सुराख़ से दोबारा नहीं डसा जाता' सबसे पहले नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से ही निकला था, फिर तो यह लोकोक्ति बन गया।
(2) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं अशअरियों की जमाअत की आवाज़ों को (उनके) क़ुरआन पढ़ने में पहचान लेता हूँ, रात में भी जब वे आते हैं। और क़ुरआन पढ़ने से रात्रि में उनकी आवाज़ों के द्वारा उनके ठिकानों को भी पहचान लेता हूँ, यद्यपि जब वे दिन को अपने ठिकानों पर उतरते हों, मैंने उन ठिकानों को देखा न हो। उनमें एक ऐसा समझदार व्यक्ति भी है कि जब (काफ़िरों के) सवारों से —या यह कहा कि— शत्रुओं से उसकी मुठभेड़ हो जाती है तो उनसे कहता है कि हमारे साथी तुमसे कहते हैं कि थोड़ी उनकी प्रतीक्षा करो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अशअरियों की प्रशंसा की कि वे अपने ठिकाने पर पहुँचकर रात में क़ुरआन पढ़ने की आवाज़ों में व्यस्त होते हैं। उनके क़ुरआन पढ़ने की आवाज़ें उनके ठिकानों का पता देती हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा शत्रु की बुराई से अपने को बचा लेता है। वह शत्रु सवारों से इस अन्दाज़ में बातचीत करता है कि वे समझते हैं कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ और लोग भी हैं। इसलिए इसपर हमला करना ख़तरे को आमन्त्रित करना है।
यहाँ यह भी ध्यान में रहे कि बुद्धिमान या विवेकी व्यक्ति का कथन भी ऐसा होता है जो ग़लत और झूठा भी नहीं होता। इसलिए ईमानवाले धर्म के शत्रुओं से लड़ने से कभी भागते नहीं। युद्ध अवश्यंभावी हो तो उसमें हिस्सा लेना उनके नज़दीक एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि उसे वे अपने लिए श्रेयकर समझते हैं।
(3) हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ज़कात लेने में ज़्यादती करनेवाला, ज़कात रोकनेवाले के सदृश है।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ज़्यादती की कई सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर वाजिब मात्रा से अधिक वसूल करे और अच्छा माल चुन-चुनकर ले या ज़कात की वुसूली में अनुचित सख़्ती से काम ले। रिवायतों में ऐसी कितनी ही मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कर्मचारी ज़कात वुसूल करते समय डरते थे और देने पर भी अच्छा माल स्वीकार करने से बचते थे, यहाँ तक कि यह स्थिति आ जाती थी कि मामला अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक पेश होता था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षा थी—
“ख़बरदार! उनके अच्छे मालों को न लेना और उत्पीड़ित की बददुआ से डरना, क्योंकि उत्पीड़ित की पुकार और अल्लाह के बीच कोई परदा और रोक नहीं है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
ज़कात में औसत दर्जे का माल लेना ही पसंद किया गया है।
ऐसा व्यक्ति ज़कात की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करनेवाला होता है, मानो वह चाहता है कि न स्वयं ज़कात दे और न दूसरों को देने दे। कोई भी व्यवस्था सफलतापूर्वक उसी समय तक चल सकती है जब तक समाज के किसी वर्ग में अरुचि, असन्तोष और शिकायत की प्रवृत्ति न पाई जाती हो। सभी एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और हितैषिता का भाव रखते हों। ऐसी स्थिति में किसी के साथ ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सकती जो उसके लिए असहनीय हो। फिर यह भी एक वास्तविकता है कि माल से फ़ायदा उठाने का हक़ सबसे पहले उसी को पहुँचता है जिसका वह माल हो। इसलिए उस पर किसी प्रकार की ज़्यादती नहीं की जा सकती।
कोई व्यवस्था सफलतापूर्वक चले इसके लिए आवश्यक है कि लोगों का उस व्यवस्था के साथ भावनात्मक लगाव हो। इस लगाव को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि इस्लामी शरीअत के आदेशों की मूल आत्मा और उसके मूल प्रयोजन की किसी स्थिति में भी उपेक्षा न की जाए। शरीअत के आदेशों और क़ानूनों पर अमल इस प्रकार हो जिसमें आदमी की मानसिकता एवं भावनाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखा जा सके।
चेतना और जागरूकता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ख़बरदार! दुनिया त्याज्य है और जो कुछ दुनिया में है वह भी त्याज्य है। सिवाय ईश-स्मरण के और उस चीज़ के जिसे वह पसन्द करता है और सिवाय ज्ञानवान और ज्ञान प्राप्त करनेवाले के।” (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : तात्पर्य यह है कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि कोई इनपर मुग्ध हो और इन्हीं को जीवन का सार समझने लग जाए। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वह इनसान की स्वाभाविक कामनाओं और उसके हौसलों से कम है। इसे पाकर सन्तुष्ट हो जाना सबसे बड़ी गुमराही और अज्ञान है। क़ुरआन में है—
“वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और सांसारिक जीवन ही पर राज़ी होकर रह गए हैं और उसी पर सन्तुष्ट हो गए और जो हमारी निशानियों से ग़ाफ़िल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है, उसके बदले में जो वे कमाते रहे हैं।" (10 : 7-8)
दुनिया में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वह है अल्लाह की याद और उसका स्मरण। वह व्यक्ति मुर्दा और चेतनारहित है जिसे सांसारिक जीवन में सब कुछ याद आया, लेकिन यदि याद न आया तो वह अल्लाह जिसने उसे पैदा ही नहीं किया, बल्कि उसकी सभी ज़रूरतों का ख़्याल भी रखा और उसे जीवन की उन तमाम ज़रूरतों के सामान भी प्रदान किए जो इनसान के हृदय में अंगड़ाइयाँ लेनेवाली कामनाओं और उसके चाह और शौक़ का एकमात्र उत्तर हैं, जिसे पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता और जिसे न पाकर इनसान अभावग्रस्त ही रहता है, चाहे देखने में वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति ही क्यों न हो।
मूल अरबी में ‘वमा वालाहु’ आया है जिसका अनुवाद “और सिवाय उस चीज़ के जिसे वह पसन्द करता है" किया गया है। इसके दो और अनुवाद किए जा सकते हैं—
(i) “और सिवाय उस चीज़ के जो अल्लाह के क़रीब करनेवाली हो।”
(ii) “और सिवाय उस चीज़ के जो उसके अधीन हो। (अर्थात् उसकी अनिवार्यताओं और अपेक्षाओं में से हो।)” 'वालाह' शब्द 'वली' से है जिसका अर्थ है प्रेम, और इसमें सामीप्य और योग का भाव भी पाया जाता है।
इस हदीस में ज्ञानवान और ज्ञान प्राप्त करनेवाले का उल्लेख मात्र उदाहरणस्वरूप किया गया है। मतलब यह है कि जो चीज़ें अल्लाह को पसन्द हैं उनमें ज्ञानवान और ज्ञान प्राप्त करनेवाले भी सम्मिलित हैं। कुछ पहलुओं से ज्ञानवान और ज्ञान प्राप्त करने में सक्रिय लोगों को जो महत्व प्राप्त है उससे सभी परिचित हैं।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुममें से जब कोई युद्ध करे तो उसे चाहिए कि वह चेहरे को बचाए (अर्थात् चेहरे पर वार न करे), क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुँह पर तमाचा मारने से भी रोका है (हदीस : मुस्लिम)। और मृत शत्रु के चेहरे को बिगाड़ने, नाक, कान आदि के काटने से भी मना किया है। (हदीस : अबू-दाऊद)
युद्ध की स्थिति में भी सूक्ष्म भावनाओं को आहत होने से बचाया जाए और उनका लिहाज़ रखा जाए। यह इस्लाम की अत्यन्त पवित्र शिक्षा है। “अल्लाह ने आदम (अलैहिस्सलाम) को अपनी सूरत पर पैदा किया है।" तात्पर्य यह है कि अल्लाह ने इनसान पर अपने गुणों की छाया डाली है। इसलिए इनसान में अल्लाह की विशेषताओं और उसके गुणों की झलक मिलती है। इनसान का चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। इनसान के चेहरे का आदर करने का आदेश अल्लाह के उन गुणों का आदर है जिनकी अभिव्यक्ति उसके चेहरे से होती है। बाइबल में भी यह वाक्य मिलता है : God created man in His own image in the image of God he created him. (Genesis: 1:27)
“ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परेमश्वर ने उसको उत्पन्न किया।” (उत्पत्ति, 1:27)
हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सूराः 'निसा' की यह आयत "अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके हक़दारों तक पहुँचा दिया करो। और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो न्यायपूर्वक फ़ैसला करो। अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है। निस्सन्देह अल्लाह सब कुछ सुनता, देखता है।" (4:58) पढ़ते तो "सबकुछ सुनता, देखता है" पढ़ते समय अँगूठे को कान पर रखते और तर्जनी को आँख पर रखते थे। (हदीस : अबू-दाऊद) इससे स्पष्ट होता है कि हमें कान और आँखें उस महान हस्ती अल्लाह से मिली जिसे स्वयं सुनने और देखने का गुण प्राप्त है। इसी प्रकार दूसरे गुण भी जो इनसान को प्राप्त हैं, वे भी वास्तव में अल्लाह ही के गुणों की प्रतिच्छाया मात्र हैं।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना— "जब कभी बन्दा कोई ऐसी बात कहता है जो ईश्वर की प्रसन्नता की होती है, और उसे इसका ध्यान भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह उसके कारण उसके दर्जे बुलन्द कर देता है। और इसी प्रकार कभी बन्दा कोई ऐसी बात कहता है जो अल्लाह को नाराज़ करनेवाली होती है, और उस व्यक्ति को इसका ध्यान भी नहीं होता, लेकिन उसके कारण वह नरक में गिर जाता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक हदीस में आता है—
“बन्दा कभी ऐसी बात मुँह से निकालता है और वह उसमें सोच-विचार से काम नहीं लेता और उसके कारण वह फिसलकर नरक में जा पड़ता है, हालाँकि वह उससे इतनी दूर होता है जितनी दूरी पूर्व और पश्चिम के मध्य होती है।" (हदीस : बुख़ारी)
इस प्रकार की हदीसों में जो बात कही गई है, आदमी यदि संवेदनशील हो तो वह उसके रहस्य को आसानी से समझ सकता है। वास्तविकता यह है कि अल्लाह और बन्दे के बीच जो सम्बन्ध पाया जाता है वह अत्यन्त नाज़ुक होता है। इस सम्बन्ध को यह अपेक्षित है कि बन्दा किसी भी मामले में और किसी भी समय अपने को ग़ैर-ज़िम्मेदार न समझे। सच्चाई आदमी का स्थान निरन्तर निश्चित करती रहती है, चाहे इससे उसकी महानता प्रकट हो या इससे उसकी अधमता प्रदर्शित हो। आदमी को चाहे इसका ख़्याल हो या न हो, उसके मुँह से निकली हुई कोई बात मात्र एक बात नहीं होती, बल्कि उससे उसके स्थान का निर्धारण भी होता है, यहाँ यह सच्चाई भी दृष्टि में रहे कि आदमी के कर्मों और आचरण के कारकों में अधिकांशतः बल्कि मूलतः भूमिका उन कारकों की होती है, जिनका सम्बन्ध उसकी चेतना से बढ़कर अचेतन से होता है। आदमी का अचेतन ही उसके कर्म और आचरण का मौलिक उद्गम होता है। आदमी हर क़दम न सोचकर उठाता है, न उठा सकता है। उसके जीवन में अचेतन का ही मूल नियन्त्रण होता है। अचेतन की संरचना में वातावरण की, और विशेष रूप से मनुष्य की अपनी भूमिका होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने अचेतन से परिचित हो। वह उसकी ओर से बेपरवाह न हो, बल्कि उसे ठीक और सही रखने का दायित्व स्वीकार करता हो।
(4) हज़रत बिलाल-इब्ने-हारिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी भलाई की कोई बात अपनी ज़बान से निकालता है और उसे उसके महत्व और दर्जे का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अल्लाह उसके कारण उसके लिए अपनी रिज़ा और प्रसन्नता उस दिन तक के लिए अनिवार्य कर देता है जबकि वह उससे मुलाक़ात करेगा। इसी प्रकार आदमी बुराई की कोई बात अपनी ज़बान से निकालता है और उसे उसकी वास्तविकता एवं उसके परिणाम का ज्ञान नहीं होता। होता यह है कि अल्लाह उसके कारण उसपर अपने प्रकोप को उस दिन तक के लिए अनिवार्य कर देता है जबकि वह उससे मुलाक़ात करेगा।” (हदीस : शरहुस्सुन्नह, मालिक, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : तात्पर्य यह है कि अल्लाह की यह रज़ामन्दी और प्रसन्नता सामयिक और स्थाई नहीं होती, क़ियामत के दिन अर्थात् अन्तिम दिवस तक के लिए होती है। तत्पश्चात् उसपर अल्लाह की जो अनुकम्पाएँ और रहमतें होंगी उनका क्या कहना! उनसे तो वह प्रत्यक्षतः लाभान्वित होगा। यहाँ यह भी दृष्टिगत रहे कि जिस व्यक्ति से ईश्वर राज़ी होता है, उससे ईश्वर के राज़ी होने का लक्षण यह है कि उस व्यक्ति को दुनिया में अच्छे कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
इसके विपरीत वह व्यक्ति जिसकी ज़बान से निकली हुई बात अल्लाह के प्रकोप को भड़का देती है, उसपर भी अल्लाह का प्रकोप सामयिक और अस्थाई नहीं होता। उसपर अल्लाह का प्रकोप क़ियामत तक जारी रहता है। आगे जहन्नम की भड़कती हुई आग उसके लिए काफ़ी होगी। यह और बात है कि कोई दुनिया में तौबा करके अपना सुधार कर ले। उसके विषय में अल्लाह का फ़ैसला बदल जाता है। वह उसकी ख़ताओं को माफ़ करके अपना निकटस्थ बन्दा बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए तौबा का दरवाज़ा बहरहाल खुला है।
इबलीस के विषय में अल्लाह ने कहा—
“और तेरे ऊपर हिसाब के दिन तक मेरी लानत है।" (क़ुरआन, 38:78)
इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि क़ियामत के दिन के पश्चात् इबलीस लानत से मुक्त हो जाएगा। उसपर अन्तिम दिन तक तो अल्लाह की लानत और फटकार है ही, आगे इस लानत के साथ नारकीय यातना की वृद्धि भी हो जाएगी, जिसे इबलीस, उसके अनुयायी और ईश्वर के दूसरे बन्दे स्वयं देख लेंगे।
तिर्मिज़ी में यह हदीस इन शब्दों में उल्लिखित है—
“तुममें से कोई व्यक्ति अल्लाह की प्रसन्नता की कोई ऐसी बात कह जाता है, और उसे गुमान भी नहीं होता कि वह उसे उस दर्जे तक पहुँचा देगी, जिस तक वह उसे पहुँचाती है। अतः अल्लाह उस बात के कारण उसके लिए अपनी रज़ामन्दी उस दिन तक के लिए लिख देता है, जब वह उससे मुलाक़ात करेगा। और तुममें से कोई व्यक्ति अल्लाह की नाराज़ी की कोई ऐसी बात कह जाता है और उसे इसका गुमान भी नहीं होता कि वह उसे उस दुर्गति तक पहुँचा देगी, जिस तक वह उसे पहुँचाती है और अल्लाह उस बात के कारण उसके लिए उस दिन तक नाराज़ी और प्रकोप लिख देता है जब वह उससे मुलाक़ात करेगा।”
(5) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा,
“श्रेष्ठतम दान यह है कि तू भूखे के जिगर को तृप्त कर दे।” (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : एक लम्बी हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रत्येक आर्द्र जिगर में अज्र है।" (हदीस : मुस्लिम)
चेतना और जीवन का सम्मान धर्म का मूल आधार है। धर्म की सारी अपेक्षाओं का सम्बन्ध जीवन और चेतना से ही है।
“श्रेष्ठतम दान यह है कि तू भूखे के जिगर को तृप्त कर दे" या “प्रत्येक आर्द्र हृदय में अज्र है" कोई साधारण वाक्य नहीं हैं, बल्कि वास्तव में ये धर्म की मूल आत्मा और उसकी प्रकृति का उत्तम चित्रण हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 'आर्द्र जिगर' कहकर जीवन और चेतना को मूर्त रूप दे दिया है कि आदमी उसे महसूस करने लगता है। 'भूखा जिगर' कहकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आदमी की अन्तर्निहित दया, सहानुभूति और वेदना के मनोभाव को उभार दिया है।
दया और सहानुभूति धर्म का सार तत्व है। इसलिए कि इसका सम्बन्ध अनुभूति की सूक्षमता से है, जो धर्म का मूल है। जहाँ कहीं जीवन और चेतना है उसका लिहाज़ अनिवार्य है। वेदना और आन्तरिक ताप से रहित व्यक्ति वस्तुतः धार्मिक भावना से वंचित है। इस बात को समझने के लिए आवश्यक है कि आदमी के भीतर चेतना और संवेदना जाग्रत हो। वह दुनिया में संवेदनहीन जीवन जीने पर सन्तुष्ट न हो।
(6) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ थे कि वर्षा होने लगी। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बाहर निकले और अपना बदन खोल दिया, यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ऊपर वर्षा (की बूँदें) पड़ीं। इसपर हमने पूछा "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसा क्यों किया?”
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा,
"इसलिए कि यह अभी ताज़ादम अपने रब के पास से आई है।" (हदीस : अबू-दाऊद, मुस्लिम)
व्याख्या : अल्लाह की नेमतों और रहमतों के पूरे एहसास के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अल्लाह की किसी अत्यन्त नई और ताज़ा रहमत का हक़ हमपर अधिक होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पूर्ण रूप से महसूस करें। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वर्षा के पानी से अपने पवित्र शरीर को भिगोकर अपनी बन्दगी और अल्लाह से अपने असाधारण सम्बन्ध को प्रकट किया। अल्लाह की योजना के अन्तर्गत पानी की जो बूँद वर्षा के रूप में गिरती है, अल्लाह और उसके बीच कोई दूसरा आड़े नहीं आता। उसका सीधा सम्बन्ध अल्लाह से होता है। वह बून्द अछूती बूँद होती है। वह अपनी प्राकृतिक पवित्रता की दशा में होती है। इसलिए वह अत्यन्त मूल्यवान और भलाई और बरकतवाली और हमारे ईमान और विश्वास का नवीनीकरण करनेवाली होती है।
तत्वदर्शिता और ज्ञान
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अबू-ख़ल्लाद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुम किसी बन्दे को देखो कि उसे दुनिया में अनासक्ति (ज़ुह्द) और मितभाषिता प्रदान हुई है तो उसका सामीप्य प्राप्त करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हृदय में तत्वज्ञान (हिक्मत) डाला जाता है।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअ्बिल ईमान)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि तत्वज्ञान एक बड़ी नेमत है, जिससे लाभान्वित होने की चाह प्रत्येक मोमिन को होनी चाहिए। तत्वदर्शिता किसी मानसिक प्रयास की उपज नहीं होती, बल्कि वह अल्लाह की ओर से उस बन्दे की ओर डाली जाती है जो सांसारिकता से विरक्त और मितभाषी होता है और मौन जिसकी वृत्ति होती है। संसार से अनासक्ति और मितभाषिता ग्रहण कर बन्दा अपने को उस स्थिति में ले जाता है कि वह परोक्ष का सम्बोधित बन सके और सत्य उसकी ओर उन्मुख हो। ऐसे व्यक्ति से लाभान्वित होकर आदमी अपने आस्वाद और प्रवृत्ति को सुधार सकता है और अपने जीवन को सँवार सकता है। अतः ऐसे व्यक्ति का सामीप्य और उसकी संगति, जिसे तत्वज्ञान मिला हो, एक जीवनदायी रसायन सिद्ध होती है। तत्वदर्शिता अपने यथार्थ की दृष्टि से एक प्रकाश और इल्हामी ज्ञान है। तत्वदर्शिता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तत्वदर्शिता दिलों में ईमान और विश्वास और मन-मस्तिष्क में विवेक और प्रज्ञा के रूप में अपना स्थान बनाती है। और व्यावहारिक जीवन में यह सज्जनता, पवित्रता, दानशीलता, कृतज्ञता और उच्च आचरण के रूप में प्रकट होती रहती है।
क़ुरआन में है—
“और जिस किसी को हिक्मत (तत्वदर्शिता) मिली, उसे बड़ी दौलत मिल गई।" (2 : 269)
तत्वदर्शिता सभी भलाइयों का स्रोत है। अल्लाह का अकृतज्ञ वही हो सकता है जो वास्तविक ज्ञान और तत्वदर्शिता से वंचित है। अल्लाह ने कहा है—
“निश्चय ही हमने लुक़मान को तत्वदर्शिता प्रदान की कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञ हो।" (31 : 12)
कृतज्ञताप्रकाशन की तरह नेकी और सत्यवादिता आदि का सम्बन्ध भी तत्वदर्शिता से है।
जिस व्यक्ति को तत्वदर्शिता की दौलत प्रदान की गई है, उसकी सगंति में रहनेवाला व्यक्ति वंचित नहीं हो सकता। वह भी उससे बहुत कुछ लाभान्वित हो सकता है। कुछ महापुरुषों का कथन है कि “ईश्वर के संग रहा करो और यदि तुममें इसकी शक्ति न हो तो फिर उस व्यक्ति की संगति में रहो जो ईश्वर के साथ रहता है।"
(2) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब किसी मुसलमान की दृष्टि किसी स्त्री के सौन्दर्य पर पहली बार पड़ जाए, फिर वह तुरन्त अपनी दृष्टि को उससे फेर ले तो निश्चय ही अल्लाह उसके लिए ऐसी इबादत प्रदान करेगा जिसका आनन्द उसे प्राप्त होगा।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : एक दूसरी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन उद्धृत हुआ है—
“निगाह के पीछे फिर निगाह न डाल (किसी स्त्री पर दृष्टि पड़ जाने के पश्चात् पुनः उसपर दृष्टि न डाल), क्योंकि पहली निगाह (जो संयोग से पड़ गई) तेरे लिए (वैध) है। दूसरी तेरे लिए वैध नहीं।” (हदीस : अबू-दाऊद, दारमी)
इसमें सन्देह नहीं कि संयोग से दृष्टि पड़ जाने के पश्चात् जो व्यक्ति दोबारा-तिबारा किसी पराई स्त्री के सौन्दर्य पर दृष्टि नहीं डालता, अल्लाह उसे वंचित नहीं रख सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यही नहीं कि ज़ाहिरी सौन्दर्य के फ़ितनों और बुराइयों से सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसके इस अच्छे कर्म के बदले में अल्लाह उसे इस ज़ाहिरी सौन्दर्य से आगे की चीज़ प्रदान करेगा, जो उससे कहीं बढ़कर मधुर, आनन्दप्रद और प्रमोदकारी होगी। उस चीज़ को हदीस में 'इबादत' का नाम दिया गया है। इबादत से अभ्रिपेत आध्यात्म ज्ञान है। 'इबादत' का यह शब्द सहीह मुस्लिम की एक हदीस में भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक विशेष स्थान पर अपने एक सहाबी को हाकिम नियुक्त करके भेजते हैं। वहाँ के लोगों को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का प्रतिनिधि किस प्रकार अल्लाह के दीन (धर्म) की ओर बुलाएगा, इस सिलसिले में निर्देश देते हुए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अतः चाहिए कि सबसे पहले जिस चीज़ की ओर तुम उन्हें बुलाओ, वह अल्लाह की इबादत है, तो जब वे अल्लाह को पहचान लें तो उन्हें इससे अवगत कराना कि प्रतापवान अल्लाह ने उनकी रात और दिन में उनपर पाँच नमाज़ें अनिवार्य की हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
इसके पश्चात् नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दूसरी अनिवार्य इबादतों ज़कात आदि के विषय में बताया कि वे किस प्रकार उनसे लोगों को अवगत कराएँ।
हदीस का जो अंश यहाँ उद्धृत किया गया है, उसमें है कि "उन्हें अल्लाह की इबादत की ओर बुलाओ। फिर जब वे अल्लाह को पहचान लें....।” इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह की इबादत की ओर बुलाने से अभिप्रेत यहाँ ईश्वर की पहचान और उसके ज्ञान का आमन्त्रण देना है। इस हदीस में इबादत से अभिप्रेत नमाज़ और ज़कात जैसे अनिवार्य कार्य नहीं, इसलिए इस हदीस में उनका उल्लेख इबादत से अलग किया गया है।
आभार प्रदर्शन
(1) हज़रत मुग़ीरा-बिन-शोअबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नमाज़ पढ़ते, यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के क़दम सूज जाते या फूल जाते। इसके विषय में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निवेदन किया जाता तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते, "क्या मैं कृतज्ञ बन्दा न बनूँ?” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा जाता कि आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं तो आप कहते कि क्या मैं अल्लाह का कृतज्ञ बन्दा न बनूँ! अर्थात इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की आवश्यकता प्रत्यक्षतः न भी हो जब भी आदमी के भीतर यदि कृतज्ञता का भाव शेष है, तो वह उसे कैसे चैन लेने दे सकता है। ऐसी स्थिति में तो आदमी चाहेगा कि वह अधिक-से-अधिक अल्लाह के सामने खड़ा हो और सजदों के द्वारा उसके असीम उपकारों के प्रति आभार प्रकट करने की कोशिश करे। अल्लाह का सबसे अच्छा बन्दा वही है जो उसका कृतज्ञ हो। कृतघ्न बनकर रहना वास्तव में आत्मा की मृत्यु है।
ईमान का सम्बन्ध इनसान के मात्र विचार और दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि उसका विशेष सम्बन्ध उसके कृतज्ञता-भाव से है। अतएव क़ुरआन में है—
“अल्लाह को तुम्हें यातना देकर क्या करना है, यदि तुम कृतज्ञ हो और (इसके फलस्वरूप) ईमान लाओ।” (4:47)
ज्ञात हुआ कि ईमान लाने से इनकार करना कृतघ्नता है। फिर इससे यह भी ज्ञात हुआ कि ईमान कोई शुष्क धारणा कदापि नहीं है, बल्कि ईमान का मामला मानव के भाव जगत् से सम्बन्ध रखता है। आप जानते हैं कि मानव के पास यदि कोई भाव न हो तो सही अर्थों में वह मानव ही नहीं है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा—
"उस सत्ता की सौगन्ध जिसके क़ब्ज़े में मेरे प्राण हैं! तुमसे इस नेमत के विषय में क़ियामत के दिन अवश्य ही पूछा जाएगा। तुम्हें भूख ने अपने घरों से निकलने पर विवश किया। फिर तुम लौटे नहीं कि यह नेमत तुम्हें प्राप्त हो गई।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस का एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है। भूख से व्याकुल होकर ये महानुभाव अपने घरों से बाहर निकल आए थे। फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ एक सहाबी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। उनके यहाँ से खा-पीकर जब वापस हुए तो उस समय अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वह बात कही जो इस हदीस में बयान की गई है।
“क़ियामत के दिन इस नेमत के विषय में पूछा जाएगा” का तात्पर्य यह है कि अल्लाह यह पूछेगा कि तुमने इस नेमत के प्रति कितना आभार प्रकट किया। इस नेमत को पाकर तुम्हारी ओर से जो उत्तम प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए, वह हुई अथवा उसे प्रकट करने से तुम असमर्थ रहे।
(3) हज़रत सअ्द-बिन-अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन का विचित्र हाल है। यदि उसे भलाई प्राप्त होती है तो यह अल्लाह की प्रशंसा करता और उसके प्रति आभार प्रकट करता है। और यदि उसे कोई मुसीबत पेश आती है तो वह अल्लाह की प्रशंसा करता और धैर्य से काम लेता है। अतः मोमिन को प्रत्येक दशा में अज्र और सवाब प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भोजन का जो ग्रास (लुक़मा) वह उठाकर अपनी पत्नी के मुँह में देता है उसमें भी उसको अज्र मिलता है।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम में हज़रत सुहैब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से इसी विषय की हदीस उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “मोमिन का मामला विचित्र है। उसका सारा ही मामला उसके लिए भलाई होता है और यह बात मोमिन के अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं। यदि उसे कोई कुशादगी और आराम पहुँचे तो आभार प्रकट करता है, तो यह उसके लिए अच्छा होता है। और यदि उसे तंगी और दुख पहुँचे तो वह सर्वथा धैर्य से काम लेता है, तो यह भी उसके लिए उत्तम होता है (अर्थात दोनों ही दशाएँ उसके लिए भलाई का कारण बनती हैं।)
जीवन में आदमी को तकलीफ़ अथवा राहत, दो ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों ही परिस्थितियों में मोमिन की ओर से उस नैतिकता का प्रदर्शन होता है जो अत्यन्त उच्च होता है। इस प्रकार वह अल्लाह की दृष्टि में प्रिय बन्दा ठहरता है। मोमिन प्रत्येक दशा में अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने में सफल होता है। यही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। इसके विपरीत ग़ैर-मोमिन व्यक्ति तकलीफ़ और दुख की दशा में साधारणतया शिकायत करने लग जाता है और सुख-सुविधा और राहत की अवस्था में अहंकारी और अल्लाह का अकृतज्ञ बन जाता है।
तकलीफ़ में धैर्य और प्रसन्नता और राहत में कृतज्ञता वास्तव में ईमान का स्पष्ट प्रमाण है। धैर्य और कृतज्ञता में कमी वास्तव में कमज़ोर ईमान का लक्षण है। यह किसी से छिपा नहीं कि कमज़ोर ईमान दृष्टिवानों की निगाह में सदैव गम्भीर चिन्ता का विषय रहा है।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति अल्लाह का भी आभारी नहीं जो इनसानों के प्रति आभार नहीं प्रकट करता।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : आभार प्रकट करने की गणना उच्च आचरणों में होती है। यह कैसे सम्भव है कि एक व्यक्ति अल्लाह का तो आभारी हो और लोगों के उसपर जो उपकार हों उनका उसे एहसास न हो। नैतिकता या चरित्र एक ऐसा गुण है जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता। कृतज्ञ व्यक्ति अल्लाह के उपकारों के साथ दूसरों की सेवाओं को भी स्वीकार करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका कोई चरित्र नहीं। उसका वह आभार प्रदर्शन भी व्यर्थ है जो वह अल्लाह के आगे करता है।
(5) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति को कोई चीज़ दी जाए और उसे सामर्थ्य प्राप्त हो तो वह अवश्य उसका बदला दे, और जिस किसी व्यक्ति को बदला देने की सामर्थ्य न प्राप्त हो तो वह देनेवाले की प्रशंसा करे, क्योंकि जिसने उपकारकर्ता की प्रशंसा की उसने उसके प्रति आभार प्रकट कर दिया और जिसने उसके उपकार को छिपाया उसने अकृतज्ञता दिखलाई।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : एहसान का बदला एहसान ही के रूप में चुकाना चाहिए। यदि कोई इस स्थिति में नहीं है कि एहसान का बदला चुका सके तो वह ज़बान से एहसान करनेवाले की प्रशंसा ही कर दे। यदि वह इतना भी नहीं करता तो उसे कृतघ्न ही कहेंगे। कृतघ्नता इनसान के आचरण पर ऐसा बदनुमा धब्बा है कि उसे किसी स्थिति में भी सहन नहीं किया जा सकता।
(6) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस किसी को कोई नेमत मिले और वह उसकी चर्चा करे तो उसने आभार प्रकट किया और जिस किसी ने उसे छिपाया उसने अकृतज्ञता दिखाई।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : किसी नेमत को पाकर कृतज्ञता दिखाना आवश्यक होता है। वह व्यक्ति मात्र जड़ है जिसे कोई नेमत मिली किन्तु उसके मन में कृतज्ञता का कोई भाव न जाग सका। उसके अकृतज्ञ होने में कोई सन्देह नहीं।
(7) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मुहाजिरों ने कहा कि—
“ऐ अल्लाह के रसूल! अनसार प्रत्येक अज्र और सवाब लूट ले गए।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“नहीं, जब तक तुम अल्लाह से उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी सराहना करते रहोगे।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अनसार ने अपने भाई मुहाजिरों के लिए असाधारण त्याग और क़ुरबानी से काम लिया था जो इतिहास में अपनी मिसाल आप है। इस पर मुहाजिरों ने सोचा कि कदाचित वे ऐसे अज्र और सवाब के अधिकारी हो गए जिसके हम अधिकारी नहीं हो सकते। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ऐसा नहीं है। यदि तुम उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हो और उनके लिए दुआ करते हो तो तुम वंचित न होगे। अन्यथा तुम्हारा एहसास सही हो सकता है।"
(8) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति जो रोज़ेदार नहीं मगर कृतज्ञ है, वह धैर्यवान रोज़ेदार जैसा है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : रोज़ेदार व्यक्ति रोज़े की अवस्था में अल्लाह के लिए धैर्य से काम लेता और खाने-पीने आदि से दूर रहता और भूख-प्यास की तकलीफ़ सहन करता है। ग़ैर-रोज़ेदार खाता-पीता और अपनी कामवासना पूरी करता है, परन्तु यदि वह अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका आभार व्यक्त करता है तो उसमें और धैर्यवान रोज़ेदार में कोई तात्विक अन्तर नहीं है। धैर्य और कृतज्ञता दोनों ही उच्च नैतिकता और चरित्र के मौलिक गुणों में से हैं। अलबत्ता यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन को धैर्य और कृतज्ञता दोनों ही के प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्तित्व अधूरा रहता है। इसी लिए मोमिनों के लिए रमज़ान के रोज़े अनिवार्य ठहराए गए हैं। यहाँ यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि वास्तव में कृतज्ञ वही व्यक्ति है जो समय पड़ने पर धैर्य व दृढ़ता का भी प्रमाण दे सके।
ख़ुशी के दिनों में जो व्यक्ति शेख़ी बघारता और इतराता है, परन्तु तंगी और मुसीबत आने पर निराशा उसे इस तरह घेर लेती है कि वह बिलकुल बुझकर रह जाता है, उसकी आत्मा धैर्य से अपरिचित है, इसी लिए वह छिछोरापन दिखाता है। धैर्य यह भी है कि आदमी अपने को छिछोरेपन और ओछेपन से दूर रखे। क़ुरआन में छिछोरेपन का चित्रण इस प्रकार किया गया है—
“यदि हम इनसान को अपनी दयालुता का आस्वादन करा कर फिर उसको उससे छीन लें तो वह निराश, अकृतज्ञ सिद्ध होता है, लेकिन यदि हम इसके पश्चात् कि उसे तकलीफ़ पहुँची हो उसे नेमत का आस्वादन कराते हैं तो वह कहने लगता है कि मेरी तो समस्त दुख-दरिद्रताएँ दूर हो गईं। वह फूला नहीं समाता, डींगे मारने लगता है। उन लोगों की बात दूसरी है जिन्होंने धैर्य से काम लिया और अच्छे कर्म किए। वही वे लोग हैं जिनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान है।” (11 : 9-11)
ज्ञात हुआ कि धैर्य के बिना जल्दबाज़ी और छिछोरेपन से आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता।
(9) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम उनकी ओर देखो जो (माल-दौलत और दर्जे में) तुमसे निम्न हैं। उन लोगों की ओर न देखो जो (सांसारिक दृष्टि से) तुमसे बढ़-चढ़कर हैं। यह तरीक़ा इस बात की प्राप्ति के लिए अधिक उचित है कि तुमपर अल्लाह की जो नेमत है वह तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ न हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : संसार में जिस व्यक्ति को बहुत कम मिला है उसे भी इतना मिला है कि उसका आभार व्यक्त करना सरल नहीं। धनवानों और समृद्धशाली लोगों की दौलत पर कोई निगाह जमाता है तो इसकी आशंका है कि स्वयं उसे अल्लाह ने अपनी दयालुता से जो कुछ दे रखा है वह उसे अत्यन्त अल्प और तुच्छ नज़र आने लगे और कृतज्ञता ज्ञापन के बजाए इसके नतीजे में उसका हृदय शिकायतों से भर जाए। यह चीज़ एक मोमिन के लिए किसी विनाश से कम नहीं। वह वस्तु जो अल्लाह के उपकारों का एहसास हमसे छीन ले, उससे बचना अत्यन्त आवश्यक है।
(10) हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दो स्वभाव ऐसे हैं जो जिस व्यक्ति में पाए जाएँगे अल्लाह उसको कृतज्ञ और धैर्यवान लिखेगा। और जिसमें वे न पाए जाएँगे अल्लाह उसे न कृतज्ञ लिखेगा और न धैर्यवान लिखेगा। जो अपने दीन (धर्म) के मामले में उस व्यक्ति को देखे, जिसे इस सिलसिले में उस पर उच्चता प्राप्त हो तो उसका अनुसरण करे। और अपनी दुनिया के मामले में उस व्यक्ति को देखे जो इस सिलसिले में उससे कमतर हो। तो इस श्रेष्ठता पर वह अल्लाह का आभार माने जो उसने उसे उस व्यक्ति के मुक़ाबले में प्रदान की है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन का सार यह है कि आदमी के धीर और कृतज्ञ होने के लिए आवश्यक है कि धर्म के मामले में वह अपने से श्रेष्ठ को देखे ताकि उसे अपने कर्म थोड़े ही महसूस हों और वह अपने से श्रेष्ठतर का अनुसरण करने के प्रयास में लग सके। लेकिन सांसारिक सुख-सुविधा की सामग्री के सिलसिले में अपने से निम्नतर पर नज़र रखे, ताकि अल्लाह के प्रति आभार प्रकट करने में कोई कमी न रह जाए। हमारे पास जो नेमतें हैं उनके नेमत होने का एहसास उस समय बहुत बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कितने ही अल्लाह के बन्दों के यहाँ उन नेमतों का अभाव पाया जाता है।
बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से भी इस प्रकार की एक हदीस उल्लिखित है जो इस प्रकार है— अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें से जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जो धन-सम्पत्ति और शारीरिक संरचना की दृष्टि से उससे बढ़कर हो, तो उसको चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को देख ले जो इन चीज़ों में उससे निम्नतम हो (ताकि लोभ-लालच के बजाए उसके अन्दर धैर्य और कृतज्ञता की भावना पैदा हो)।”
(11) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन बन्दे से नेमतों के विषय में जो पहला प्रश्न होगा वह यह कि उससे कहा जाएगा कि क्या हमने तेरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान नहीं किया था और तुझे ठण्डे पानी से तरोताज़ा नहीं किया था?" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में दो प्रकट नेमतों का उल्लेख किया गया है, जिनका नेमत होना प्रत्येक व्यक्ति को भली-भाँति मालूम है। इसलिए इनके विषय में सबसे पहले प्रश्न होगा। प्रश्न का तात्पर्य यह है कि इनसान से यह पूछा जाएगा कि जिस अल्लाह ने तुझे ये नेमतें प्रदान की थीं, तूने उसके प्रति आभार प्रकट किया या नहीं? अल्लाह ने इनसान को जीवन और चेतना प्रदान की है, अतः उसका कर्तव्य है कि अल्लाह की नेमतों और उसके उपकारों के प्रत्युत्तर में उत्तम प्रतिक्रिया व्यक्त करे, अर्थात् उसका हार्दिक रूप से कृतज्ञ हो।
जीवन की नेमतों को पाकर हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम अपने उपकारकर्ता को पहचानें और उसकी इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त करें। इनसान को दुनिया में जो नेमतें प्राप्त हैं, वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि इन नेमतों को प्रदान करनेवाला अल्लाह रहमतों और बरकतोंवाला है। उसने ये नेमतें प्रदान करके इनसानों से अपना गहरा सम्बन्ध दर्शाया है। हमारा सम्बन्ध जितना अपने शरीर और प्राण से है, उससे कहीं अधिक उस बरकतवाली सत्ता से है, जो हमारे अस्तित्व और जीवन का मूल कारण है। वह यदि हमसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर ले तो हम विनष्ट हो जाएँगे। अल्लाह अपने बन्दों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। उनपर उसकी दयालुता और अनुकम्पा की छाया सदैव पड़ती रहती है। उसकी यह अनुकम्पा सबके लिए है। सोचने की बात यह है कि क्या अल्लाह की प्रदान की हुई नेमतों को पाकर हमने यह जानने का प्रयास किया कि इन नेमतों को देनेवाला कौन है? क्या उसके प्रदानों और अनुकम्पाओं का यह अर्थ नहीं कि हम उससे हार्दिक रूप से अपना सम्बन्ध स्थापित करें और उसके प्रति सर्वथा कृतज्ञ बन जाएँ? नेमतों के विषय में पूछे जाने का तात्पर्य यही होता है कि इन नेमतों से लाभान्वित होने के पश्चात् हमारी ओर से द्रोह, बेवफ़ाई और संवेदनहीनता का प्रदर्शन हुआ या हम उसके कृतज्ञ और आज्ञाकारी बन्दे बनकर रहे। क़ुरआन में कहा गया है—
“फिर निश्चय ही तुमसे उस दिन नेमतों के विषय में पूछा जाएगा।" (81:8)
(12) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सुबह होती है तो तुममें से प्रत्येक व्यक्ति के हर जोड़ पर सदक़ा वाजिब होता है। अतः प्रत्येक 'तसबीह' एक सदक़ा है और प्रत्येक 'तहमीद' एक सदक़ा है और हर 'तहलील' एक सदक़ा और हर "तकबीर" एक सदक़ा है, भलाई का हुक्म देना एक सदक़ा है और बुराई से रोकना एक सदक़ा है, और इन सबके बदले में वे दो रकअतें (नमाज़) काफ़ी हो जाती हैं जिनको बन्दा चाश्त के समय (दिन चढ़े) अदा कर लेता है। " (हदीस : मुस्लिम, अबू-दाऊद)
व्याख्या : “हर जोड़” के लिए मूल में "सुलामा" शब्द प्रयुक्त हुआ है। “सुलामा" जोड़दार छोटी हड्डियों को कहते हैं, जैसे अंगुलियों की हड्डियाँ। इस शब्द का बहुवचन "सुलामियात" होता है। फिर अर्थविस्तार के कारण प्रत्येक हड्डी को सुलामा कहा जाने लगा। और यह शब्द हड्डी के जोड़ों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा।
तसबीह, तहमीद, तहलील और तकबीर का अर्थ क्रमशः यह है— सुब्हा-नल्लाह (महान है अल्लाह), अलहम्दुलिल्लाह (स्तुति अल्लाह ही के लिए है), ला इला-ह इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य-प्रभु नहीं) और अल्लाहु अकबर (महान है अल्लाह) कहना।
हम देखते हैं कि आदमी को प्रतिदिन अल्लाह की ओर से एक नया जीवन मिलता है। गुज़रे हुए कल की तरह उसे फिर एक दिन प्राप्त होता है। यह जीवन अल्लाह की असीम अनुकम्पाओं और अनुग्रहों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस हदीस में उदाहरण के रूप में मानव शरीर की प्रत्येक हड्डी और जोड़ का उल्लेख एक नेमत की हैसियत से किया गया है। अल्लाह की हर नेमत और उसकी दी हुई प्रत्येक चीज़ का अर्थ होता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। चाहिए तो यह कि बन्दा दान और सदक़े के द्वारा ईश्वर के प्रत्येक उपकार पर कृतज्ञता दिखाए, क्योंकि अपनी भावनाओं में सच्चे होने का यह स्पष्ट प्रमाण होता। लेकिन अल्लाह की यह विशेष कृपा है कि उसने तसबीह और तहमीद आदि के शब्दों और नेक कर्मों को सदक़ा घोषित कर दिया है। इस प्रकार बन्दे के लिए यह सम्भव हो सका कि वह ईश्वर के उपकारों का आभार मानने की स्थिति में हो सके।
फिर हम जानते हैं कि चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ कोई अनिवार्य नमाज़ नहीं है। यह नमाज़ बताती है कि बन्दा अनिवार्य नमाज़ों पर ही बस नहीं करता, बल्कि ईश्वर से उसका विशिष्ट सम्बन्ध अपनी तृप्ति चाहता है। इसके लिए वह अतिरिक्त नमाज़ का सहारा लेता है। ईश्वर से इस प्रकार के लगाव के प्रदर्शन में यदि दिखावा नहीं सच्चाई है, तो वह सारे ही सदक़ों का बदल है। सदक़ा ईश्वर से विशेष लगाव का ही प्रदर्शन है और यह चीज़ यहाँ अत्यधिक विद्यमान है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को सारे सदक़े अदा करके अल्लाह के इनामों और उपकारों का आभार प्रकट करने का अवसर मिल न सका तो चाश्त की नमाज़ ही उन सारे सदक़ों के बदले में पर्याप्त होगी।
सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से भी इसी प्रकार की एक हदीस उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रत्येक दिन सूरज निकलता है तो इनसान के शरीर में जितने जोड़ हैं उनमें हर एक की ओर से एक सदक़ा आवश्यक होता है। (यह सदक़ा इस प्रकार अदा हो सकता है कि) दो आदमियों के बीच किसी मामले में फ़ैसला करा दिया, यह भी एक सदक़ा है। किसी व्यक्ति की उसकी अपनी सवारी पर सवार होने के सिलसिले में सहायता कर दी और उसे उसपर सवार करा दिया, यह भी एक सदक़ा है या उसका सामान उठाकर ऊपर रख दिया, यह भी एक सदक़ा है। पवित्र और भली बात भी एक सदक़ा है और प्रत्येक क़दम जो नमाज़ के लिए जाने को उठाया जाए, एक सदक़ा है। और रास्ते से किसी कष्टप्रद चीज़ को हटा दिया तो यह भी एक सदक़ा है।"
इस हदीस से मालूम हुआ कि तसबीह, तहमीद और नमाज़ ही नहीं, बल्कि हर नेक काम जो इनसान कर सकता है वह सदक़ा ठहरता है, शर्त यह है कि उसका वह नेक काम ईश्वर के यहाँ स्वीकृत हो जाए।
किसी छोटे-से-छोटे भले और अच्छे काम को तुच्छ न समझने के कई कारण हो सकते हैं :
(i) नेकी चाहे देखने में छोटी और हल्की क्यों न हो, यदि उसके पीछे ईमान की सच्ची भावना विद्यमान है तो वह मूल्यवान है। उसका अपमान वस्तुतः ईमानी भावना का अपमान है।
(ii) कोई भी नेक काम हो उससे इसका पता लगता है कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। किसी ने कहा है कि चुटकी भर धूल का क्या महत्व? लेकिन उससे पता चलता है कि हवा का रुख़ क्या है?
(iii) प्रत्येक योग्यता समान नहीं होती और न दुनिया में काम करने के सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए अपनी योग्यता और अवसर की दृष्टि से आदमी जो भी काम करता है वह ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होता है, यहाँ तक कि सदक़े में खजूर का एक टुकड़ा देना भी किसी के लिए जहन्नम की आँच से बचाने के लिए पर्याप्त हो सकता है।
(iv) छोटी नेकी के मूल्यांकन की योग्यता यदि हममें पाई जाएगी तो हम ईश्वर से अच्छी आशा कर सकते हैं और नैतिकता की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। इसके विपरीत यदि हम केवल बड़े काम को ही काम समझें तो निराशा का शिकार होने से हम अपने आपको नहीं बचा सकते।
(v) पुष्प चाहे छोटे हों या बड़े, वे पुष्प हैं, निगाहों को भले लगते हैं। किसी भी पुष्प का तिरस्कार पूरी पुष्प-जाति का तिरस्कार है।
(vi) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उस शिक्षा को, जिसका उल्लेख इस हदीस में हुआ है, अपनाने के पश्चात् हमारी दृष्टि में प्रत्येक वह व्यक्ति सम्मानित ठहरेगा जो अपनी योग्यता की दृष्टि से कोई नेक और अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वह काम देखने में छोटा ही क्यों न हो।
(vii) जीवन को सुन्दर बनानेवाले और उसे ठीक रखनेवाले एवं लोगों के लिए आकर्षण का कारण बननेवाले काम साधारणतः ऐसे ही होते हैं जो देखने में छोटे होते हैं, परन्तु वे सामाजिकता और इस्लामी संस्कृति के प्राण होते हैं।
(viii) आदमी की सही पहचान उन्हीं कामों के द्वारा होती है जो देखने में महत्वहीन और छोटे नज़र आते हैं। कोई आदमी कैसा है? यह जानने के लिए उसके मुख से निकली एक छोटी और संक्षिप्त-सी बात ही काफ़ी हो सकती है। आदमी की जुबान पर आई हुई एक बात या उसका छोटा-सा कर्म भी ऐसा होता है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित करता है। इस प्रकार एक छोटा-सा वाक्य अथवा कर्म या तो उसके बड़प्पन को प्रदर्शित करता है या फिर उसकी निम्नता और अधमता को। रूपवान चेहरे से यदि ज़रा भी पर्दा हट जाए तो उसका सौंदर्य प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भले आदमी का एक छोटा कर्म भी उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी होता है।
कर्म जहाँ हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को प्रकट करते हैं, वहीं उनके द्वारा हमारे अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। इस सिलसिले में छोटी से छोटी नेकी भी अपनी भूमिका निभाती है।
गुण ग्राहकता
(1) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी भी अच्छे काम को तुच्छ न समझो यद्यपि वह काम यही हो कि तुम अपने भाई से प्रसन्न मुद्रा में मिलो।” (हदीस : मुस्लिम)
सच्चाई
(1) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि वह अत्यन्त सच्चा हो जाता है। और झूठ दुष्कर्म और मर्यादाहीनता की ओर ले जाता है, और यह मर्यादाहीनता नरक की ओर ले जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वह ईश्वर के यहाँ बड़ा झूठा लिख लिया जाता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मुस्लिम की एक हदीस में यह भी आया है—
“सच्चाई, वास्तव में नेकी और वफ़ादारी है। और निश्चय ही नेकी और वफ़ादारी जन्नत में पहुँचाती है।”
आदमी में यदि सच्चाई नहीं तो उसपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वह विश्वसनीय नहीं रहा तो फिर किसी नेकी और वफ़ादारी की उससे क्या आशा की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की उस जन्नत का अधिकारी कैसे हो सकता है जो उन लोगों के ठहरने की जगह है जो नेक और वफ़ादार होते हैं।
बुख़ारी और मुस्लिम की एक हदीस में है—
“आदमी सच बोलता रहता है और ढूँढ-ढूँढकर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि ईश्वर के यहाँ वह अत्यन्त सच्चा लिख लिया जाता है। और आदमी झूठ बोलता रहता है और तलाश-तलाशकर झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि ईश्वर के यहाँ वह बड़ा झूठा लिख लिया जाता है।"
सच्चाई पर क़ायम रहनेवाला और सदैव सच बोलनेवाला ईश्वर के यहाँ सिद्दीक़ (सत्यवान) की उपाधि पाता है। क़ुरआन मजीद में नबियों के पश्चात् “सिद्दीक़ों" का उल्लेख किया गया है (क़ुरआन, 4:69)। इससे अन्दाज़ा होता है कि सिद्दीक़ नैतिकता और चरित्र के अत्यन्त उच्च स्थान पर होता है। जिस किसी व्यक्ति की नीति यथार्थपरक हो उसे इस उच्च स्थान पर पहुँचने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। क़ुरआन में कहा गया है—
“वफ़ादारी और नेकी केवल यह नहीं है कि तुम अपने मुँह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि वफ़ादारी तो उसकी वफ़ादारी है जो ईश्वर, अन्तिम दिन, फ़रिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाया और माल, उसके प्रति प्रेम के बावजूद, नातेदारों, अनाथों, मुसाफ़िरों और माँगनेवालों को दिया और गर्दनें छुड़ाने में भी, और नमाज़ क़ायम की और ज़कात दी और ऐसे लोग अपने वचन को पूरा करनेवाले हैं जब वचन दें; और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में और लड़ाई के समय जमनेवाले हैं, ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे सिद्ध हुए और वही लोग डर रखनेवाले हैं।" (2:177)
इस आयत से स्पष्ट होता है कि ईश्वर की दृष्टि में सच्चा वह है जो हर मामले में और हर अवसर पर सच्चा सिद्ध हो सके।
जिस प्रकार सच्चा व्यक्ति नेकियों और भलाइयों का स्रोत है ठीक उसी प्रकार झूठ सभी प्रकार के दुष्कर्मों और दुराचारों की जड़ है। ऐसा व्यक्ति जिसने झूठ को अपनी नीति बना रखा होता है, बुराई के कामों में उसे कोई झिझक नहीं होती। अन्ततः वह नरक में जा गिरता है और ईश्वर के यहाँ उसकी गणना झूठों और बड़े झूठों में होती है। ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र व आचरण की दृष्टि से महाझूठा होता है और ईश्वर के यहाँ भी उसे यही उपाधि मिलती है।
(2) हकीम-बिन-हिज़ाम (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्रय-विक्रय करनेवाले दोनों अधिकार रखते हैं जब तक परस्पर एक-दूसरे से पृथक न हों। यदि दोनों सच बोलें और चीज़ की वास्तविक हालत बयान कर दें तो उनके लिए उनकी बिक्री में बरकत प्रदान की जाती है। यदि वे छिपाएँ और झूठ से काम लें तो उनकी बिक्री की बरकत समाप्त कर दी जाती है।"
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि क्रय-विक्रय करनेवाले जब तक एक-दूसरे से अलग न हों उन्हें सौदे को रद्द करने का अधिकार रहता है। अलग होने के पश्चात् सौदा रद्द करने का अधिकार शेष नहीं रहता, यह दूसरी बात है कि क्रय-विक्रय करनेवालों के मध्य ऐसी कोई बात निश्चित हो चुकी हो जिसकी दृष्टि से दोनों के अलग होने के पश्चात् भी सौदे को रद्द करने का अधिकार बना रहता है। अधिकार के कई रूप और प्रकार हैं, जिनका सम्बन्ध समय-सीमा से है और कुछ बेची जानेवाली चीज़ों की कोटि से सम्बन्धित हैं। फ़िक़्ह (इस्लामी धर्मशास्त्र) की पुस्तकों में इनका विशद विवेचन देखा जा सकता है।
इस हदीस से प्रकटतया यह मालूम होता है कि जब तक दोनों पक्ष एक-दूसरे से अलग नहीं होते तब तक उन्हें किए हुए सौदे को रद्द करने का अधिकार होता है। किन्तु कुछ लोगों का कहना यह है कि हदीस में एक-दूसरे से अलग होने की जो बात कही गई है उसका अर्थ यह है कि जब तक सौदे की बात-चीत चल रही है और मामला पूरे तौर पर अभी तय नहीं हो सका है, उन्हें इसका अधिकार है कि वे सौदे को रद्द कर दें। लेकिन बात यदि पूरी हो गई और एक ने कहा कि मैंने बेचा और दूसरे ने कहा कि मैंने ख़रीदा तो सौदे को रद्द करने का अधिकार शेष नहीं रहता सिवाए इसके कि माल में कोई ऐसा दोष आदि निकल आए जिसे ख़रीदार को नहीं बताया गया था। उसे उसकी सूचना न थी।
विलग होना दो प्रकार का होता है। एक स्थान की दृष्टि से है और दूसरा बात और दिए हुए वचन की दृष्टि से। इस दूसरे की मिसाल भी क़ुरआन में मिलती है। क़ुरआन में है— “यदि दोनों (स्त्री-पुरुष) अलग ही हो जाएँ तो ईश्वर अपनी समाई से प्रत्येक को बेनियाज़ कर देगा।" (4:130)
यहाँ अलग होने से अभिप्रेत स्त्री को तलाक़ दे देना है, मजलिस या घर से अलग होना नहीं। सौदे में भलाई और बरकत दोनों ही पक्ष के लिए रखी गई है, शर्त यह है कि वे मामले में सच्चाई की नीति अपनाएँ, अन्यथा वे भलाई व बरकत से वंचित रहेंगे।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"सिद्दीक़ (अत्यन्त सत्यवान) के लिए शोभनीय नहीं कि वह बहुत लानत करनेवाला हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : सिद्दीक़ नबियों के पद चिन्हों पर चलते हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आदर्श सदैव उनकी दृष्टि में रहता है। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) न अश्लील भाषी थे, न लानत करनेवाले और न ही अपशब्द बोलनेवाले थे (बुख़ारी)। सही मुस्लिम में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! बहुदेववादियों के हक़ में बददुआ कीजिए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुझे लानत करनेवाला बनाकर नहीं भेजा गया है बल्कि मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है।"
सिद्दीक़ों के दिलों में भी ईश्वर के बन्दों के प्रति हितैषिता का भाव पाया जाता है। विरोधियों की ओर से वे तकलीफ़ सहन करते हैं परन्तु उनकी कामना और सबसे बढ़कर इच्छा यही होती है कि लोग सत्यमार्ग पर आ सकें। उनका यह स्वभाव नबियों से मिलता-जुलता है। उनके हृदयों की दशा यह होती है कि वे अपने शत्रु के भी हितैषी होते हैं। उन पवित्र हस्तियों के लिए यह कैसे उचित हो सकता है कि ईश्वर के बन्दों को फटकारें और उनपर लानत भेजें।
परितोष
(1) हज़रत इब्ने-मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन का पाठ किया, “अतः जिस किसी का ईश्वर मार्गदर्शन करना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है" (6:124)। फिर कहा, "जब प्रकाश सीने में प्रविष्ट हो जाता है तो सीना विस्तीर्ण हो जाता है।" पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस दशा का प्रकट रूप से कोई लक्षण भी है जिससे उसे पहचाना जा सके? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, हाँ, धोखे के घर (दुनिया) से दूर होना और शाश्वत घर की ओर रुजू करना तथा मृत्यु आने से पूर्व उसके लिए तैयार रहना।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : क़ुरआन मजीद में भी दुनिया के बारे में कहा गया है—
“अतः सांसारिक जीवन तुम्हें कदापि धोखे में न डाले।” (31:33)
दुनिया और आख़िरत को हदीस में दो सौतनों की उपमा दी गई है कि यदि उनमें से एक प्रसन्न हो तो दूसरी उससे रुष्ट व नाराज़ हो जाती हो। एक की ओर झुकाव हो तो आवश्यक है कि दूसरी की ओर झुकाव न हो। दुनिया, जो धोखे का घर है, से अनासक्ति और आख़िरत की ओर झुकाव का सम्बन्ध वस्तुतः हार्दिक भाव से है। इसी लिए इनको हृदय में प्रकाश के प्रवेश करने का परिणाम और लक्षण कहा गया है। प्रकाश भी वास्तव में एक भाव ही का नाम है। यह साधारण विज्ञानों और धारणाओं से आगे की चीज़ें हैं। इनके बिना इनसान को पूर्णत्व और आत्मिक विकास सही अर्थ में प्राप्त नहीं हो पाता।
विश्वास और ईमान
(1) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता से और वे अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इस उम्मत की प्रथम भलाई विश्वास और सार से अनासक्ति है, और प्रथम बिगाड़, कृपणता, अनुचित आशा और कामना है।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : विश्वास और संसार से अनासक्ति, इन दोनों में परस्पर बड़ा गहरा सम्बन्ध पाया जाता है, बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों चीज़ें सभी प्रकार की भलाइयों और कल्याण की स्रोत हैं। व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उम्मत अर्थात मुस्लिम समुदाय का कल्याण भी इसी पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखने की चीज़ यही है कि इस भलाई के स्रोत से उम्मत किस सीमा तक लाभान्वित हो रही है। उम्मत को जब तक ईश्वर की सत्ता पर यह विश्वास और भरोसा होगा कि वह उसका पालनकर्ता और संरक्षक है, दिखाए हुए मार्ग पर चलकर वह सफलता प्राप्त कर सकती है, वह कभी भी ग़लत नीति नहीं अपनाएगी। कोई भी जो सांसारिकता से अपने को दूर रखेगा और सांसारिक लोभ और मोह के बजाए पारलौकिक जीवन का इच्छुक होगा, उसे कोई चीज़ सत्यमार्ग से विचलित नहीं कर सकती। इस दृष्टि से संसार से अनासक्ति की बड़ी महत्ता है। संसार से अनासक्ति का अर्थ वास्तव में यह होता है कि महत्वपूर्ण चीज़ के प्रकाश में तुच्छ चीज़ की तुच्छता उद्घाटित हो जाए। दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में तुच्छ है। दुनिया की प्राप्ति के लिए आख़िरत की उपेक्षा करना अविश्वास, नीचता और जड़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
कृपणता, अनुचित कामनाएँ और आशाएँ, ख़राबी और बिगाड़ के प्राथमिक लक्षण हैं। कृपणता और सांसारिकता के साथ उम्मत के लिए उस मार्ग पर चलना सम्भव नहीं जो उत्तम समुदाय अर्थात समुदाय के लिए नियत किया गया है। कृपणता और दुनिया की आशाएँ और कामनाएँ उसे उस महान कार्य के योग्य नहीं रहने देतीं जो उसे दुनिया में अन्जाम देना है और जिसके लिए ईश्वर ने उसे इस धरती पर पैदा किया है। कृपणता, लोभ, कामना और दुनिया प्राप्त करने की इच्छा की कोख से अनगिनत बुराइयाँ और ख़राबियाँ जन्म लेती हैं, जिनका सामान्य परिस्थितियों में आदमी को आभास तक नहीं होता। उम्मत में जब आप देखें कि कृपणता और सांसारिकता की बीमारी पैदा हो गई है तो समझ जाइए कि उसकी तबाही और विनाश का आरम्भ हो चुका है। यदि वह अपनी नीति नहीं बदलती तो बुरे अन्जाम से दोचार होने से उसे कोई नहीं बचा सकता।
(2) हज़रत-इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा और ईमान दोनों परस्पर निकट रखे गए हैं। इनमें से जब एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है।"
हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत के शब्द ये हैं—
“जब इनमें एक का हरण हो जाता है तो दूसरा भी उसी का अनुसरण करता है (अर्थात् उसका भी हरण हो जाता है)।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : लज्जा और ईमान में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। मोमिन को जिस सत्य पर विश्वास होता है और वह जिसपर ईमान रखता है, उसकी अपेक्षा केवल यही नहीं कि मनुष्य केवल अपने विचार और बाह्य कर्मों को सँवारे, बल्कि इससे बढ़कर यह भी अपेक्षित है कि वह अपने मनोभावों, अनुभूतियों और अन्तर्मन तक का सुधार करे। लज्जा की प्रकृति अत्यन्त कोमल होती है। यह इनसान की सूक्ष्मतम अनुभूतियों का प्रदर्शन है। “लज्जा ईमान की एक शाखा है" (बुख़ारी, मुस्लिम)। फिर ईमान को एक शुष्क कल्पना कैसे कहा जा सकता है। हदीस का सारांश यह है कि यदि लज्जा नहीं तो ईमान कैसे ठहर सकता है? इसी प्रकार यदि ईमान चला गया तो फिर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति में किसी से इसकी आशा नहीं की जा सकती कि वह लज्जावान सिद्ध होगा।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"बहुत-से बिखरे बालोंवाले, धूल-धूसरित लोग, जिन्हें दरवाजों से धक्के देकर हटा दिया जाता है, ऐसे हैं कि यदि वे (किसी बात के लिए) ईश्वर की सौगन्ध खा लें तो निश्चय ही ईश्वर उनकी सौगन्ध पूरी कर दे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : एक-दूसरी लम्बी हदीस में भी यह बात इन शब्दों में कही गई है—
"ईश्वर के कुछ बन्दे ऐसे हैं कि यदि वे ईश्वर की सौगन्ध खा लें तो निश्चय ही ईश्वर उसे पूरा करे।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम) अर्थात् उनको उनकी क़सम में सच्चा कर दे। जिस बात की वे क़सम खा लें वह पूरी होकर रहे।
हदीस का अर्थ यह है कि ईश्वर के ऐसे बन्दे भी होते हैं कि जिनका विश्वास ऐसा होता है कि ईश्वर उसे सच्चा कर दिखाता है। यदि वे अपने विश्वास और इत्मीनान पर ईश्वर की सौगन्ध खा लें तो उनकी क़सम झूठी नहीं होती। ईश्वर उनके विश्वास की रक्षा करता है। इसकी भी सम्भावना है कि ऐसे लोगों को सामान्यतः न पहचाना जा सके और वे लोगों को तुच्छ दीख पड़ें। बड़े लोग उन्हें पसन्द न करें, जब वे उनके दरवाज़े पर आएँ। परन्तु ईश्वर की दृष्टि में वे ऐसे प्रिय और स्वीकृत और उँचे दर्जेवाले होते हैं कि ईश्वर उनके गुमान व विश्वास को रद्द नहीं करता, बल्कि उनकी क़समों को पूरा करके उन्हें सच्चा सिद्ध कर देता है।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस व्यक्ति के अन्दर तीन बातें मौजूद होंगी वह ईमान के माधुर्य का आस्वादन करेगा— ईश्वर और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बढ़कर उसे कोई प्रिय न हो, वह किसी व्यक्ति से प्रेम करे तो केवल ईश्वर के लिए प्रेम करे, कुफ़्र (इनकार) की ओर पलटना इसके पश्चात् कि ईश्वर ने उसको नजात दी, उसे ऐसा अप्रिय और असहनीय हो जैसा कि वह आग में झोंक दिए जाने को अप्रिय और असहनीय समझता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में पूर्ण ईमान और विश्वास की पहचान बता दी गई है। पूर्ण ईमान में ऐसा आस्वादन और माधुर्य विद्यमान रहता है कि उसे शब्दों में बयान करना सम्भव नहीं है। पूर्ण ईमान उस व्यक्ति का होता है जो ईश्वर और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सबसे बढ़कर प्रेम करे। फिर किसी दूसरे से यदि प्रेम करता भी है तो वह केवल ईश्वर के लिए। अर्थात् यदि ईश्वर को पसन्द हो कि उस व्यक्ति से प्रेम का सम्बन्ध रखा जाए तभी वह उससे प्रेम करता है। कुफ़्र की ओर लौटने को ऐसा बुरा समझे मानो उसे आग में झोंका जा रहा हो।
इससे यह भी मालूम हुआ कि ईमान इनसान की गहरी और सूक्ष्मतम भावनाओं एवं भावों को प्रभावित करता और उन्हें निखारता है। ईमान ईश्वर और उसके रसूल को केवल मानने का नाम नहीं है, बल्कि वस्तुतः उन्हें अपना प्रिय बना लेने का नाम है। ऐसे प्रिय जिनसे बढ़कर कोई भी प्रिय न हो। ईमान की ज़िन्दगी सर्वथा प्रेम की ज़िन्दगी होती है, ऐसी ज़िन्दगी पर हज़ारों सौन्दर्य निछावर हों।
एक और हदीस में ईमान के भाव को इन शब्दों में बयान किया गया है—
"ईमान का आस्वादन कर चुका वह व्यक्ति जो ईश्वर के पालनकर्ता प्रभु, इस्लाम के धर्म और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रसूल होने पर राज़ी और प्रसन्न हो गया।" (हदीस : मुस्लिम)
सत्य का आदर
(1) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर का गौरवगान करो, वह तुम्हें क्षमा कर देगा।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : क़ुरआन में है "तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईश्वर के लिए गौरव की आशा नहीं रखते।" (71:13)
ईश्वर की महानता और उसके गौरव को स्वीकार करने का मतलब है कि इनसान अपने आपको ईश्वर की महानता के आगे नत कर दे और अपने आप को उसकी आज्ञापालन और उसकी बन्दगी में दे दे। उसकी महानता व बड़ाई को स्वीकार करे। अपने स्रष्टा के गौरवगान में स्रष्टा की पवित्रता को सदैव ध्यान में रखे और उसके बन्दों, विशेषतः उसके आज्ञापालकों के अधिकारों को पहचाने। अतएव एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन ईश्वर कहेगा—
“वे लोग कहाँ हैं जो मेरे प्रताप के कारण परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करते थे? आज मैं उन्हें अपनी छाया में जगह दूँगा, मेरी छाया के अतिरिक्त आज और कोई छाया नहीं।" (हदीस : मुस्लिम)
ईश्वर के प्रताप और उसकी महानता का आदर करनेवालों को ईश्वर क्षमा कर देगा। ईश्वर कोई जड़ सत्ता नहीं है कि बन्दा तो उसकी महानता के आगे झुक जाए और वह अपने बन्दे की आवश्यकता की उपेक्षा करे। निश्चय ही वह ऐसे बन्दों की भूल-चूक क्षमा करेगा और उसे अपनी दयालुता से ढक लेगा।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क़ियामत के दिन ईश्वर कहेगा कि कहाँ हैं वे लोग जो मेरी सहायता और मेरे प्रताप के कारण परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करते थे? आज जबकि मेरी छाया के अतिरिक्त कोई छाया नहीं, मैं उन्हें अपनी छाया में स्थान दूँगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि ईश्वर की महानता का एहसास मात्र एक एहसास ही नहीं है बल्कि यह एहसास इनसान की ज़िन्दगी को एक नवीन चेतना प्रदान करता है, जिसके कारण इनसानी ज़िन्दगी में ऐसी गहराई, उच्चता और पवित्रता आ जाती है और ज़िन्दगी एक ऐसे आनन्द से परिचित हो जाती है जिसकी सामान्य अवस्था में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। दुनिया में यूँ तो लोग एक-दूसरे से प्रेम और सम्बन्ध रखते ही हैं लेकिन उस प्रेम-सम्बन्ध की बात ही और है जिसके पीछे ईश्वर की महानता का एहसास काम कर रहा है और जो ईश्वर की बड़ाई का तक़ाज़ा बनकर सामने आए।
ईश्वर के इस कथन से कि "वे लोग कहाँ हैं जो परस्पर एक-दूसरे से मेरी महानता के कारण प्रेम करते थे" अभिप्रेत वास्तव में उन्हें सम्मान प्रदान करना है।
क़ियामत के दिन जिनको ईश्वर की दयालुता और उसके अर्श (राजसिंहासन) की छाया मिल गई वे अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करें कम है। उस दिन जिन्हें ईश्वर की छाया न मिल सकी उन्हें कोई भी छाया प्राप्त न होगी। कोई न होगा जो उस दिन उनके लिए किसी छाया की व्यवस्था कर सके। उस दिन सारे झूठे सहारे समाप्त हो चुके होंगे। यह ऐसा दिन होगा कि असत्य का असत्य होना भली-भाँति स्पष्ट हो जाएगा। झूठे ख़ुदाओं के माननेवालों के हिस्से में उस दिन भय, पछतावा और लज्जा के अतिरिक्त कुछ न आ सकेगा।
(3) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस बन्दे ने ईश्वर के लिए किसी बन्दे से प्रेम किया तो निश्चय ही उसने अपने गौरववान प्रभु की बड़ाई की।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : इससे मालूम हुआ कि हम ईश्वर की महानता का लिहाज़ नहीं रखते यदि हमें उन लोगों से कोई हार्दिक प्रेम नहीं जिनसे हमें ईश्वर के लिए प्रेम करना चाहिए। मोमिन का किसी से प्रेम मात्र प्रेम नहीं है, बल्कि यह पालनकर्ता प्रभु की बड़ाई का प्रदर्शन भी है। क्या ही अच्छा है वह प्रेम जिसका सिलसिला गौरववान प्रभु से मिल रहा हो!
(4) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"किसी बूढ़े मुस्लिम का सम्मान करना और क़ुरआन के ऐसे ज्ञानी का सम्मान करना जो क़ुरआन में दोनों प्रकार की अतियों से बचता हो, वास्तव में ईश्वर ही का सम्मान करना है। इसी प्रकार न्यायशील शासक का सम्मान करना भी ईश्वर ही का सम्मान है।" (हदीस : अबू-दाऊद, बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : जो व्यक्ति क़ुरआन का ज्ञाता और हाफ़िज़ हो और उसके हक़ों को पहचानता हो वह आदर का पात्र है। इसी प्रकार वह शासक जो न्याय की अपेक्षाओं को न भूलता हो उसका सम्मान करना भी हमारे लिए आवश्यक है। क़ुरआन ईश्वरीय वाणी होने के कारण सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है। न्यायप्रिय शासक का न्याय ईश्वर की न्यायशीलता को व्यक्त कर रहा होता है, इसलिए ईश्वर की बड़ाई को यह अपेक्षित है कि क़ुरआन के ज्ञाता और न्यायप्रिय शासक दोनों ही का सम्मान किया जाए।
इसी प्रकार वह मुस्लिम भी सम्मान के योग्य है जो बुढ़ापे को पहुँच गया। उसके प्रति आदर का कारण मात्र बुढ़ापा नहीं, बल्कि वह लम्बी उम्र है जो मोमिन के रूप में गुज़री है।
यह हदीस बताती है कि ईश्वर सदैव एक मुस्लिम की निगाह में रहता है। ज़िन्दगी का सलीक़ा वह उसी से सीखता है। वह जीवन में जो भी नीति अपनाता है ईश्वर के लिए ही अपनाता है। यही वास्तव में वह दर्जा है जिसे 'एहसान' कहा गया है और जिसे प्राप्त करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुममें से कोई दुआ माँगे तो यूँ न कहे कि ऐ अल्लाह! यदि तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, बल्कि ताकीद के साथ आग्रहपूर्वक दुआ करे और अपने साहस एवं इच्छा को बुलन्द रखे, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रदान करना अल्लाह के यहाँ कुछ भारी नहीं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : शर्त के साथ दुआ माँगनी कि “ऐ ईश्वर! तू चाहे तो इसे क़ुबूल कर और चाहे तो क़बूल न कर" किसी तरह भी सही नहीं। क्योंकि इस तरह से दुआ माँगने में बन्दे की बेनियाज़ी प्रकट होती है जो वास्तविकता के विपरीत और भक्ति भावना के प्रतिकूल है। यदि वह अपनी नादानी में ईश्वर की सुविधा के विचार से शर्त के साथ दुआएँ माँगता है तो भी यह निरर्थक और ईश्वर की शान में एक गुस्ताख़ी है, क्योंकि ईश्वर के लिए तो कोई काम भी कठिन नहीं कि उसकी सुविधा का ख़्याल रखा जाए। ईश्वर की शान तो यह है कि वह अपने बन्दे को जो चाहे प्रदान करे, इसमें उसके लिए कोई कठिनाई नहीं।
(6) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर के मुखारबिन्द का वास्ता देकर केवल जन्नत ही माँगी जा सकती है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ईश्वर के प्रताप का वास्ता देकर अथवा इसके बदले में कुछ चाहने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कहीं इससे ईश्वर के मुखारबिन्द का निरादर न हो रहा हो। जिस व्यक्ति के समक्ष प्रतापवान ईश्वर का सौन्दर्य हो, उसे उससे कम दर्जे की किसी चीज़ के माँगने का ख़याल कैसे आ सकता है। हाँ ईश्वर के मुखारबिन्द का वास्ता देकर अगर कोई चीज़ माँगी जा सकती है तो वह केवल जन्नत है। यह इसलिए कि जन्नत में वस्तुतः ईश्वर का सामीप्य और उसके दर्शन प्राप्त होंगे।
ईश्वर की रिज़ा और प्रसन्नता
(1) हज़रत साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"यह आदम के बेटे के सौभाग्य में से है कि ईश्वर की ओर से उसके लिए जो भी फ़ैसला हो वह उसपर राज़ी रहे। और यह आदम के बेटे के दुर्भाग्य में से है कि वह ईश्वर से भलाई माँगना छोड़ दे और आदम के बेटे का हतभाग्य यह भी है कि ईश्वर का जो फ़ैसला उसके हक़ में हो उसपर वह अप्रसन्न हो।" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : आदमी नहीं जानता कि उसके हक़ में क्या भला है और क्या बुरा। उसे प्रत्येक दशा में ईश्वर के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। यही उसके लिए सौभाग्य की बात है। यद्यपि उसके प्रभु के यहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं। वह अपने प्रभु से सदैव भलाई की प्रार्थना करता रहे। इस प्रकार अपने प्रभु से उसका सम्बन्ध भी बना रहेगा। यह सम्बन्ध असाधारण सौभाग्य की बात होगी। क़ुरआन में है—
“और बहुत सम्भव है कि किसी चीज़ को तुम नापसन्द करो और वह तुम्हारे लिए उत्तम हो, और बहुत सम्भव है कि किसी चीज़ को तुम पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। ईश्वर जानता है, तुम नहीं जानते।” (2 : 226)
वह व्यक्ति बड़ा अभागा है जो ईश्वर के फ़ैसले पर राज़ी और सन्तुष्ट न हो, बल्कि उसपर नाराज़ और अप्रसन्न हो। उसे शिकायत हो कि ईश्वर ने उसके लिए जो फ़ैसला किया है वह उसे पसन्द नहीं। ऐसे व्यक्ति को शान्ति और परितोष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ यह सच्चाई भी दृष्टि में रहे कि ईश्वर से सम्बन्ध और उसका प्रेम ऐसी चीज़ है कि इसे पाकर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। कहा गया है—
"अजब चीज़ है लज्ज़ते-आशनाई” (प्रेम का आस्वादन विचित्र चीज़ है)।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ अबू-सैफ़ हद्दाद के यहाँ गए, जो (अल्लाह के रसूल के सुपुत्र) इबराहीम की धाय के पति थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इबराहीम को गोद में लिया। फिर उनको चूमा और उन्हें सूँघा। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात् हम फिर उनके यहाँ गए। इबराहीम उस समय मरणासन्न दशा में थे। यह देखकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखों से आँसू आ गए। इसपर अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा “ऐ अल्लाह के रसूल! आप भी रोते हैं।” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “ऐ इब्ने औफ़! यह रहमत है।" इसके पश्चात् आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखों से फिर आँसू बहने लगे और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "आँखें आँसू बहा रही हैं और हृदय शोकाकुल है लेकिन इसके बावजूद हम वही कहेंगे जिससे हमारा प्रभु राज़ी और प्रसन्न हो सके, और ऐ इबराहीम! हम तेरी जुदाई से शोकाकुल हैं।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अबू-सैफ़ का नाम बराअ् था। उनकी पत्नी ख़ौला-बिन्त-मुन्ज़िर अन्सारिया थीं जो ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बेटे इबराहीम की धाय थीं। इबराहीम की 16 अथवा 17 माह की अवस्था में मृत्यु हुई।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने प्यार में इबराहीम के मुँह पर अपनी नाक और मुँह को इस प्रकार रखा जैसे कोई ख़ुशबू सूँघता है। मतलब यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बच्चे को ख़ूब प्यार किया।
अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ ने जो कुछ कहा उसका अर्थ यह था कि दुखद अवसर पर साधारण लोग तो अवश्य रो देते हैं किन्तु आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तो ईश्वर के पैग़म्बर हैं। आपकी आँखें आँसू बहाएँ, हमें इसपर आश्चर्य हो रहा है।
हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जवाब देते हुए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जो चीज़ तुम देख रहे हो वह रहमत है।" अर्थात् यह रोना दयाभाव के कारण है। ये आँसू दया और प्रेम के कारण बहे हैं। ये शिकायत के आँसू कदापि नहीं हैं। ईश्वर के फ़ैसले पर राज़ी रहना भक्ति और बन्दगी की अपेक्षाओं में से है। ऐसे अवसर पर आँखें न भीगें तो यह कठोर हृदयता का प्रतीक है। कठोर हृदयता पैग़म्बर तो क्या, आम इनसान के लिए भी बड़े ऐब की बात है।
हज़रत इबराहीम की मरणासन्न दशा में जो कुछ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा उससे प्रकट होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को हज़रत इबराहीम की जुदाई का शोक और दुख भी है, आँखों में आँसू भी आ गए हैं, और हृदय शोकाकुल भी है, किन्तु इसके बावजूद ज़बान पर कोई शिकायत नहीं। यहाँ मानवता की पराकाष्ठा के साथ बन्दगी की पराकाष्ठा का प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी का नाम 'रिज़ा' है जो सौभाग्य का उच्च स्थान है। अतएव हदीस में है कि यह आदमी के सौभाग्य में से है कि ईश्वर ने उसके लिए जो फ़ैसला कर दिया हो वह उसपर राज़ी हो। (हदीस : तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद)
अमानतदारी
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (अपने धार्मिक अभिभाषणों में) ऐसा कम ही सम्बोधन किया होगा जिसमें यह न कहा हो—
“उस व्यक्ति में ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं और वह व्यक्ति बे दीन है जो वचन का पाबन्द नहीं।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : एक दूसरी हदीस में विश्वासघात और वचनभंग की गणना कपटाचार में की गई है। इस हदीस से पता चलता है कि ईमान और दीन का आदमी के चरित्र और जीवन के मामलों से गहरा सम्बन्ध है। ईमान की अपेक्षा यह है कि आदमी अमानतदार हो और धर्म आदमी को वचन का पाबन्द बनाता है। यदि किसी व्यक्ति में अमानतदारी नहीं तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति ईमानी अपेक्षाओं से बेख़बर और उसका दिल ईमान के रसास्वादन से अपरिचित है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को दिए हुए वचन की पाबन्दी नहीं करता तो अभी वह धर्म के वास्तविक मनोविज्ञान को नहीं समझता। धर्म आदमी को ईश्वर का बन्दा और उसका आज्ञाकारी बनाता है। अब यदि कोई किसी इनसान को दिए हुए अपने वचन के पालन में असमर्थ है तो फिर वह अपने पूरे जीवन में उस महान प्रण का निर्वाह कैसे कर सकता है जिसके अनुसार उसे अपना सम्पूर्ण जीवन ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार व्यतीत करना है।
ईश-भय
(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"कोई भी चीज़ ईश्वर को दो बूँदों और दो निशानों से बढ़कर प्रिय नहीं है। एक बूँद उन आँसुओं की है जो ईश्वर के भय से निकलें और दूसरी बूँद उस रक्त की है जो ईश्वर के मार्ग में गिराया जाए। रहे दो निशान तो उनमें से एक निशान तो वह है जो ईश्वर के मार्ग में पड़े और दूसरा निशान वह है जो ईश्वर के निर्धारित किए हुए अनिवार्य कार्यों में से किसी कार्य के पूरा करने में लगे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : आँसुओं की वे बूँदें जो ईश-भय से गिरती हैं, ईश्वर को सबसे बढ़कर प्रिय होती हैं या रक्त की वे बूँदें सबसे बढ़कर प्रिय होती हैं जो ईश्वर के मार्ग में लड़ते हुए घायल या शहीद होने से गिरती हैं। ईश्वर के भय से गिरी हुई आँसुओं की बूँदें इनसान की आन्तरिक पवित्रता और सज्जनता को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार ईश्वर के मार्ग में गिरी हुई रक्त की बूँदें इस बात की गवाही देती हैं कि बन्दे ने दुनिया में जो जीवन अपनाया वह ईशपरायणता का जीवन था। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बन्दा वह सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गया था जो उसे प्राप्त था। यहाँ तक कि उसे अपने प्राण न्योछावर करने में भी कोई संकोच न हुआ। इस पूर्ण समर्पण और वफ़ादारी पर यदि ईश्वर को प्यार न आएगा तो किस चीज़ पर आएगा।
ईश्वर के मार्ग में पड़े निशान और प्रभाव से तात्पर्य क़दमों या ज़ख़्मों आदि के निशान हैं। इसी प्रकार अनिवार्य कर्मों के पूरा करने के निशान से संकेत कई चीज़ों की ओर हो सकता है, जैसे—हज में क़दमों का गर्द से अट जाना, रोज़े के कारण शारीरिक कमज़ोरी और मुँह की बू आदि, नमाज़ी के चेहरे की आभा जो अपने रब से वार्तालाप और उसे सजदा करने के कारण उसके चेहरे से प्रकट होती है। क़ुरआन में आया है—
“वे अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं जिनपर सजदों का प्रभाव है।" (48:29)
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर के भय से रो पड़नेवाला नरक में दाख़िल नहीं हो सकता, जब तक कि (थन से निकला हुआ) दूध थन में वापस न हो जाए और ईश्वर के मार्ग की धूल और नरक का धुआँ एकत्र न होंगे।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार थन से निकाला हुआ दूध थन में वापस नहीं होता, उसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति का नरक में दाख़िल होना असम्भव है जो ईश-भय से दुनिया में रो पड़ा हो शर्त यह है कि यह रोना रस्मी और दिखावे का न हो। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति दुनिया में ईश्वरीय मार्ग में संघर्षरत रहा और ईश्वर के मार्ग में उसे धूल और ग़ुबार और विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसे पारलौकिक जीवन में नरक के धुएँ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर से यह आशा नहीं की जा सकती कि जिस व्यक्ति ने दुनिया में सत्यमार्ग में गर्द-ग़ुबार और परेशानियों का स्वागत किया, वह जब ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो तो वहाँ उसके हिस्से में नरक का धुआँ और आग की लपटें आएँ। दुनिया की परेशानियाँ आख़िरत की परेशानियों से निश्चिन्त और सुरक्षित रहने की ज़मानत हैं। यह ईश्वर के गौरव के प्रतिकूल है कि उसका फ़ैसला किसी व्यक्ति के हक़ में यह हो कि दुनिया में तो वह ईश्वरीय मार्ग में प्रयासरत रहे और राह की धूल और ग़ुबार उसके हिस्से में आए और जब वह आख़िरत की दुनिया में दाख़िल हो तो नरक का धुआँ उसकी तक़दीर बन जाए। यह तो अत्यन्त निष्ठुरता और संवेदनहीनता की बात होगी।
धूल और धुएँ में समरूपता है। इसी लिए कहा गया है कि ईश्वर के मार्ग की धूल और नरक का धुआँ दोनों एकत्र नहीं हो सकते, अर्थात् किसी के हिस्से में दोनों चीज़ें नहीं आ सकतीं। अब यह हमपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि जहन्नम और उसके धुएँ से नजात मिल सके तो फिर हमको ईश्वरीय मार्ग की धूल और ग़ुबार और इस राह में पहुँचनेवाली तकलीफ़ों और परेशानियों को अपनाना होगा।
यह हदीस इस पहलू से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें मोमिन (ईमानवाले व्यक्ति) के दिल की दुनिया और उसके बाह्य जीवन दोनों ही पर रौशनी डाली गई है। यह हदीस बताती है कि मोमिन का दिल ईश-भय के एहसास से परिपूर्ण होता है और उसके व्यावहारिक जीवन का रुख़ क्या है, इसकी जानकारी उस सक्रियता से मिलती है जो ईश्वरीय मार्ग में वह दिखा रहा होता है।
(3) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दो आँखें ऐसी हैं जिनको नरक की आग नहीं छू सकती— एक वह आँख जो ईश्वर के भय से रो पड़ती हो और दूसरी वह आँख जिसने ईश्वर के मार्ग में पहरा देते हुए रात व्यतीत की हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इनसान के सामने एक बड़ा ख़तरा है। वह ख़तरा है नरक की यातना का। यह ख़तरा किस प्रकार टल सकता है? यह एक बुनियादी प्रश्न है। इसी का जवाब हमें इस हदीस में मिलता है।
आराम और मुसीबत दो परिचित सत्य हैं। सहज स्वभाव के अनुकूल जो चीज़ें होती हैं वे आराम और सुख-सुविधा का कारण बनती हैं। और जो चीज़ें हमारे सहज-स्वभाव के प्रतिकूल होती हैं वे हमारे लिए मुसीबत और यातना का कारण होती हैं। दुनिया में आदमी आराम और तकलीफ़ दोनों ही से दोचार होता है। दुनिया में दोनों चीज़ें मिली-जुली-सी हैं लेकिन वास्तव में दोनों चीज़ें सहजातीय नहीं हैं। जिस प्रकार हर चीज़ का एक स्रोत होता है ठीक उसी प्रकार आराम और राहत का भी कोई स्रोत होना चाहिए। यह वही स्रोत है जिसे स्वर्ग कहते हैं। और मुसीबत और तकलीफ़ का मूल स्रोत नरक है। जिस तकलीफ़ और मुसीबत का कमतर रूप हम दुनिया में देखते हैं, उसके बड़े स्वरूप से भी इनसान दोचार हो सकता है। इसी प्रकार आराम और सुख-सुविधा के सीमित रूप यहाँ दिखाई देते हैं, उनका पूर्ण रूप भी सामने आ सकता है। मानव जीवन जिन चिन्हों और लक्षणों से आच्छादित होता है यदि आदमी उसमें सोच-विचार से काम ले तो इस बात को समझने में उसे कोई कठिनाई न होगी कि सुख-सुविधा हो या तकलीफ़, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर एक जीवन्त सत्ता है। उसके गुणों और उसकी नीति का प्रदर्शन हमारे जीवन में निरन्तर होता रहता है। ईश्वर यदि अपने बन्दों के लिए आराम और सुख-सुविधा का प्रबन्ध करता है तो वह उन्हें यातना देना भी जानता है।
दुनिया में तकलीफ़ों से बचने के लिए इनसान विभिन्न उपाय करता है। उदाहरण के रूप में, गर्मी से बचने के लिए छाया जुटाता है। वातानुकूलित मकान के अन्दर रहता है। सर्दी से बचने के लिए वह गर्म कपड़े पहनता है। लेकिन उस बड़ी तकलीफ़ से बचने के लिए जो नरकाग्नि के रूप में आएगी क्या उपाय हो सकता है? वास्तविकता यह है कि इस सिलसिले में एक उपाय के अतिरिक्त सारे ही उपाय निष्फल सिद्ध होंगे। वह उपाय यह है कि ईश्वर की कृपा-दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए इस हदीस में दो चीज़ों का उल्लेख किया गया है—
प्रथम, ईश-भय जिसकी गवाही नम आँखों ने दी हो और दूसरी जागती हुई आँखें जिन्होंने ईश्वर के मार्ग में पहरा दिया हो। ईश्वर की दयालुता से यह परे है कि वह उन आँखों को यातना दे जिनसे ईश-भय के कारण आँसू बहे हों अथवा जो ईश्वर के मार्ग में जाग्रत रही हों।
प्रत्येक मामले में शुद्ध-हृदयता का मूल महत्व है। आप इसे भली-भाँति समझ सकते हैं कि हृदय की यह विशुद्धता विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है। इसलिए कभी एक चीज़ को बन्दे की नजात और मुक्ति का कारण ठहरा दिया जाता है तो कभी किसी दूसरी चीज़ को उसके मुक्त होने का प्रमाण कहा जाता है।
एक मोमिन जो रातों में ईश्वर के लिए पहरा देता है, उससे इसकी आशा नहीं की जा सकती कि वह विश्वासघाती और अनुत्तरदायी होगा। इसी प्रकार ईश्वर के भय से रोनेवाले व्यक्ति से इसकी आशा नहीं की जाएगी कि वह एक ओर तो ईश्वर के भय से आँसू बहाएगा, लेकिन दूसरी ओर ईश्वर और उसके बन्दों के हक़ छीनने में उसे कोई संकोच न होगा। यदि यह बात है तो न वह आँसू बहाने में सच्चा है और न ही रात को पहरा देने में। कर्म कोई भी हो वह उसी समय विश्वसनीय समझा जाता है जबकि वह बन्दे के वास्तविक चरित्र का प्रतीक हो। ऐसा न हो कि इसके पीछे प्रसिद्धि और नामवरी की इच्छा अथवा इसी प्रकार की कोई दूसरी भावना कार्यरत हो।
यह हदीस हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को सच्चरित्र बनाएँ। हममें ईमानदारी हो और हमारे अपने कर्म ऐसे हों कि उनके साथ नरक में जाना सम्भव ही न हो सके।
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से क़ुरआन की इस आयत “और जो लोग देते हैं (ज़रूरतमन्दों को) जो कुछ देते हैं और हाल यह होता है कि दिल उनके काँप रहे होते हैं" (23:60) के विषय में पूछा कि क्या ये वे लोग हैं जो शराब पीते हैं और चोरी करते हैं? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "नहीं, ऐ सिद्दीक़ की बेटी! बल्कि ये वे लोग हैं जो रोज़े रखते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और सदक़े देते हैं और इसके बावजूद डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनके ये कर्म अस्वीकृत हो जाएँ। यही वे लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : इस हदीस में जिस आयत का उल्लेख किया गया है वह आयत और उसके आगे की आयत यह है—
“और जो लोग देते हैं (ज़रूरतमन्दों को) जो कुछ देते हैं और हाल यह होता है कि दिल उनके काँप रहे होते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने रब की तरफ़ पलटना है। यही वे लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही उनके लिए अग्रसर रहनेवाले हैं।” (23:60-61) आयत में देने की जो बात कही गई है तो इससे अभिप्रेत केवल माल देना ही नहीं है, बल्कि आज्ञापालन का अर्थ भी इसमें पाया जाता है।
इस हदीस में है कि उनके दिल काँप रहे होते हैं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को ख़याल हुआ कि उनके दिलों के काँपने और ईश्वर से डरने का कारण शायद यह हो कि उन्होंने बुरे काम किए हों, उदाहरणार्थ वे शराब पीते हों और चोरी करते हों। यदि वे नेक काम करते होते तो उनके डरने का प्रत्यक्षतः कोई कारण न था।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बताया कि इस आयत में जिन लोगों का उल्लेख किया गया है वे किसी दुष्कर्म के शिकार कदापि नहीं हैं, बल्कि वे सारे अनेक कर्म करते हैं। लेकिन वे अपनी सामर्थ्य भर करके भी डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारे कर्म ईश्वर की दृष्टि में स्वीकृत होंगे या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर के यहाँ इनमें कुछ दोष निकल आए और ये नेकियाँ रद्द कर दी जाएँ। डरने का वास्तविक कारण गुनाह के काम नहीं, बल्कि उनकी शराफ़त और वह एहसास है जो ईश्वर की महानता और उसके अधिकारों के महत्व के विषय में उनमें पाया जाता है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आयत का जो अर्थ बताया, उसकी पुष्टि आयत में वर्णित प्रसंग से ही हो जाती है कि उन्हीं पवित्र आत्माओं के विषय में ईश्वर का कथन है कि “यही वे लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही इन (भलाइयों) के लिए अग्रसरता दिखानेवाले हैं।" स्पष्ट है कि भलाइयों में जल्दी करनेवाले और उनके लिए अग्रसरता दिखानेवाले लोग गुनाहों में लिप्त नहीं हो सकते।
(5) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन अपने गुनाहों को इस प्रकार देखता है जैसे वह किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और डर रहा हो कि कहीं वह उसके ऊपर न गिर पड़े। (इसके विपरीत) दुराचारी और बदकार व्यक्ति अपने गुनाहों को इस प्रकार देखता है जैसे कोई मक्खी हो जो उसकी नाक पर से गुज़रती है।" (रावी ने) कहा कि वह ऐसे कर देता है (उड़ा देता है)। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ईमान की अपेक्षा यह है कि आदमी गुनाहों को हल्का कदापि न समझे। उसे गुनाहों से इस प्रकार भयभीत होना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और उसे यह आशंका हो कि कहीं पहाड़ उसके सिर पर न गिर पड़े और उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके विपरीत दुराचारी और बदकार व्यक्ति गुनाहों की कुछ भी परवाह नहीं करता। उसकी दृष्टि में गुनाह की हैसियत ऐसी होती है जैसे कोई मक्खी उसकी नाक के पास से गुज़रे, जिसे वह सरलता से उड़ा सके।
इस हदीस में जो उपमा प्रस्तुत की गई है वह अत्यन्त प्रभावकारी है। इस उपमा के द्वारा ईमानवाले और दुराचारी व्यक्ति दोनों की जीती-जागती तस्वीर स्पष्ट होकर हमारे सामने आ जाती है। इससे हम भली-भाँति जान सकते हैं कि ईश्वर से डरनेवालों के हृदय की दशा क्या होती है और उन लोगों की क्या मानसिकता होती है जिनके दिलों में किसी प्रकार का भय नहीं होता, जो अत्यन्त निर्भयतापूर्वक बड़े से बड़ा अपराध करते हैं।
परहेज़गारी
(1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने एक व्यक्ति की इबादत और (इस सिलसिले में) उसके प्रयास और परिश्रम का उल्लेख किया गया और एक अन्य व्यक्ति की परहेज़गारी का उल्लेख किया गया। इसपर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "इस (इबादत और परिश्रम) को परहेज़गारी के समान न ठहरा।” 'रि-अ-तुन' का अर्थ परहेज़गारी है। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इससे मालूम हुआ कि बाह्य इबादत और तप और परिश्रम में कोई कितना ही बढ़ा हुआ क्यों न हो वह उस व्यक्ति के समान नहीं हो सकता जो अपने जीवन में आत्मसंयम और परहेज़गारी का विशेष ख़याल रखता हो। कारण स्पष्ट है कि जीवन के मामलों में परहेज़गारी की नीति वही व्यक्ति अपना सकता है जिसे ईश्वर की महानता और उसके प्रति अपनी जवाबदेही का पूरा एहसास हो। दोनों व्यक्तियों में जो तात्विक अन्तर पाया जाता है उसकी किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं की जा सकती।
मूल पाठ में "रिअतुन" शब्द आया है। किसी रावी ने स्पष्टीकरण करते हुए इसका मतलब परहेज़गारी बताया है।
(2) हज़रत अबू-मुहम्मद हसन-बिन-अली-बिन-अबू-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सुनी हुई यह बात मुझे अच्छी तरह याद है—
“जो बात तुम्हें सन्देह में डाले उसे छोड़कर वह बात अपनाओ जो तुम्हें किसी सन्देह में न डाले। क्योंकि सच्चाई सर्वथा शान्ति और निश्चिन्तता और झूठ सर्वथा सन्देह और संशय है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : एक दूसरी हदीस में है—
"जिस बात पर जी को इत्मीनान हो और दिल जिस पर टिक जाए वह नेकी है और जो जी में खटकने और दिल में उलझन और संशय का कारण हो वह गुनाह है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, दारमी)
नेकी का विशेष गुण यह है कि इससे दिल को शान्ति और निश्चिन्तता का एहसास होता है। वह दिल में काँटा बनकर नहीं खटकती और न किसी प्रकार के सन्देह एवं दुविधा में ग्रस्त करती है। इसलिए ऐसी बातों से दूर रहना आवश्यक है जिनमें नेकी की विशेषता न पाई जाती हो। मोमिन का दिल सत्य का मानदण्ड होता है। उसकी अभिरुचि स्वयं उसे सूचित करती रहती है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि संयम और परहेज़गारी की नीति का आदर वही लोग कर सकते हैं जिनकी अभिरुचि शुद्ध हो और वे अपने प्राकृतिक संवेदनों के मूल्य को पहचानते हों। वे उसे किसी भौतिक हित के लिए कदापि त्याग नहीं सकते।
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-इब्ने-यज़ीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कोई बन्दा ईश्वर का भय रखनेवालों में सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि वह गुनाह में पड़ने के भय से उस चीज़ को न छोड़ दे जिसमें कोई गुनाह नहीं।” (हदीस : तिर्मिजी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : किसी जाइज़ चीज़ से वंचित रह जाने में कुछ ऐसा हर्ज नहीं। परन्तु यदि कोई अवैध कर बैठा तो यह उसके लिए गम्भीर बात होगी। यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे सज़ा के मामले में हम सब जानते हैं कि अपराधी सज़ा पाने से बच जाए तो यह उतना बुरा नहीं है जितना कि किसी निर्दोष को सज़ा दे दी जाए। इसी लिए सन्देह का लाभ सदैव मुलज़िम को पहुँचता है। अतः यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि नाजाइज़ चीज़ों से बचा रहे तो उसे अत्यन्त सावधानी से काम लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि इस सावधानी के परिणामस्वरूप कुछ जाइज़ चीज़ें भी उससे छूट सकती हैं, लेकिन ईश-भय और परहेज़गारी के स्थान को पाने के लिए उसे इसे स्वीकार करना होगा। मैमून-बिन-महरान के अनुसार हराम से बचने और उससे दूर रहने के लिए आवश्यक है कि हम हलाल की अन्तिम सीमा तक न जाकर और उसके एक हिस्से को छोड़कर अपने और हराम के मध्य विशेष दूरी बनाए रखें।
यहाँ ध्यान रहे कि सन्दिग्ध के विषय में अधिक बारीकी और सूक्ष्मता से काम लेना उसी व्यक्ति को शोभा देता है जो स्पष्ट बुराइयों से बचता हो। परन्तु वह व्यक्ति जो खुले तौर पर गुनाहों में लिप्त रहता हो उसे यह चीज़ शोभा नहीं देती कि वह संयम और परहेज़गारी की बारीकियाँ निकालता फिरे। उसे मसीह (अलैहिस्सलाम) के शब्दों में यही कहा जाएगा कि मच्छर छानता है लेकिन ऊँट को निस्संकोच निगल जाता है।
(4) हज़रत अबू-अब्दुल्लाह नोमान-बिन-बशीर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“(धर्म में) हलाल भी स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है। यद्यपि इन दोनों के बीच कुछ बातें सन्दिग्ध हैं जिनको अकसर लोग नहीं जानते। अतः जो इन सन्दिग्ध मामलों से बचता रहे, उसने अपने धर्म और अपनी इज़्ज़त की ओर से सफ़ाई पेश कर दी। और जो सन्दिग्ध मामलों में पड़ गया वह हराम चीज़ों में भी ग्रस्त होकर रहेगा। यह बिलकुल ऐसा है जैसे कोई चरवाहा किसी वर्जित क्षेत्र के आस-पास अपने जानवरों को चराता रहे तो इसकी सम्भावना अधिक है कि उसके जानवर उसमें जा पड़ें। सुन लो! प्रत्येक सम्राट का कोई न कोई वर्जित क्षेत्र होता है और ईश्वर का वर्जित क्षेत्र उसकी निर्धारित वर्जनाएँ हैं। सुन लो! शरीर में माँस का एक लोथड़ा होता है, जब वह ठीक हुआ तो पूरा शरीर ठीक हो गया और जब वह बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ गया। सुन लो! वह (माँस का लोथड़ा) हृदय है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : ऐसे मामलों में, जिनके वर्जित या अप्रिय होने की आशंका हो, सावधानी आवश्यक है। इसकी सम्भावना है कि कुछ सन्दिग्ध मामलों के विषय में किसी विद्वान को इसकी खोज हो कि उनके सम्बन्ध में इस्लामी शरीअत का क्या आदेश है। ऐसे व्यक्ति को इस सिलसिले में अपने शोध को व्यवहार में लाने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु जिन लोगों को उनके विषय में शरीअत का आदेश मालूम नहीं है, उन्हें उन मामलों से परहेज़ की नीति अपनाने ही में भलाई है। यदि वे सन्दिग्ध मामलों के सिलसिले में बेपरवाही से काम लेते हैं और उनके प्रति सावधान नहीं रहते तो इसकी सम्भावना है कि वे कभी हराम कार्यों में ग्रस्त हो जाएँ। हराम से बचने के लिए आवश्यक है कि सन्दिग्ध मामलों में बेपरवाही से काम न लिया जाए, बल्कि जहाँ तक सम्भव हो उनसे अपने को दूर रखा जाए। जिनके जानवर वर्जित चरागाह से दूर रहकर चरते हैं वे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो लोग अपने जानवरों को चराने के लिए वर्जित क्षेत्र के किनारे तक ले जाते हैं, तो इसकी अधिक आशंका है कि उनके जानवर किसी भी समय वर्जित चरागाह के अन्दर प्रवेश कर जाएँ। धर्म में वर्जनाओं की हैसियत वर्जित क्षेत्र की है। उसमें प्रवेश करने से बचने के लिए आवश्यक है कि हम उसके निकट भी न जाएँ।
इस मामले में परहेज़गारी और सावधानी से काम वही व्यक्ति ले सकता है जो एक स्वस्थ हृदय का मालिक हो। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि हृदय के ठीक होने और उसकी सलामती पर ही शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारे कर्म ठीक हों इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को ठीक रखें। हृदय यदि अन्य के प्रेमपाश से मुक्त है और वह एक ईश्वर का हो गया है तो निश्चय ही इनसान सन्दिग्ध चीज़ों की ओर क़दम नहीं उठा सकता। लेकिन हृदय यदि अन्य के प्रेमपाश से मुक्त नहीं है तो उसके यहाँ एकाग्रता और ईश्वर की ओर रुजू होने का कोई अवसर ही नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ हृदय कदापि नहीं कहा जा सकता है। इस दशा में सन्दिग्ध तो क्या, मनुष्य घोर अवैध कार्यों में भी लिप्त हो सकता है।
निर्विकार हृदय सभी भलाइयों का स्रोत और अपने आप में बड़ी नेमत है। क़ुरआन में है—
“जिस दिन न माल काम आएगा और न सन्तान सिवाय इसके कि कोई भला-चंगा दिल लेकर ईश्वर के पास आया हो।” (26:88-89)
भले चंगे दिल की क्या पहचान है, इसके लिए क़ुरआन की ये आयतें देखें—
“और जन्नत परहेज़गारों के निकट लाई जाएगी, कुछ भी दूर न होगी। कहा जाएगा : यह है वह चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस व्यक्ति के लिए जो बहुत रुजू करनेवाला और बड़ी निगरानी करनेवाला था, जो बिना देखे रहमान से डरता था और जो आसक्त हृदय लिए हुए आया है।" (50:31-33)
ज्ञात हुआ कि भला-चंगा दिल वही हो सकता है जो ईश्वर के प्रति आसक्त हो, जो ईश्वर की ओर निरन्तर प्रवृत्त रहता हो और ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रेमी न हो।
(5) हज़रत नोमान-बिन-बशीर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“हलाल भी स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है। यद्यपि इन दोनों के बीच कुछ चीज़ें सन्दिग्ध हैं। अतः जो व्यक्ति उन गुनाहों से बचेगा जो उसके लिए सन्दिग्ध हैं, वह खुले गुनाहों से तो सबसे बढ़कर बचेगा। और जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के करने में दुस्साहस दिखाएगा जिनके गुनाह होने का संशय हो, उसके खुले गुनाहों में पड़ जाने की अधिक आशंका है। गुनाहों की दशा वर्जित क्षेत्र की है, और जो वर्जित क्षेत्र के आस-पास चरता है उसके उसमें जा पड़ने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस के शब्दों से हदीस संख्या 4 का अर्थ भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है।
(6) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुच्छ और साधारण गुनाहों के सिलसिले में सावधान रहना, क्योंकि ईश्वर की ओर से इनकी भी पूछ होगी।" (हदीस : इब्ने-माजा, दारमी, बहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : साधारण गुनाहों को सामान्यतः लोग हल्का समझते हैं और उनसे बचने के लिए अधिक सावधानी नहीं बरतते। यद्यपि वे भी गुनाह हैं और उनके करने से भी ईश्वर के आदेश का उल्लंघन होता है। जिन लोगों को आख़िरत की पकड़ का ख़याल बना रहता है वे बड़े गुनाहों से ही नहीं छोटे गुनाहों से भी बचने की पूरी कोशिश करते हैं और चिन्तित रहते हैं। जिन लोगों के दिलों में ईश्वर का भय और उसकी महानता का एहसास होता है उनकी निगाह में छोटे गुनाह भी कुछ कम ख़तरनाक नहीं होते। जो गुनाह भी ईश्वर की अप्रसन्नता का कारण बने, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उससे बचना आवश्यक है। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते थे—
"तुम लोग बहुत-से ऐसे कर्म करते हो जो तुम्हारी निगाह में बाल से भी अधिक बारीक (अर्थात् बहुत ही हल्के) होते हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के समय में हम उनकी गणना घातक चीज़ों में करते थे।" (हदीस : बुख़ारी)
मतलब यह है कि वे उनको भी अत्यन्त घातक समझते थे और उनसे बचने की पूरी कोशिश करते थे।
जिस प्रकार छोटे गुनाहों को हल्का समझना सही नहीं, क्योंकि दाग़ छोटा हो या बड़ा वह दाग़ ही है, इससे अपने दामन को पाक रखकर ही हम अपनी सुरुचि का प्रमाण दे सकते हैं, ठीक इसी प्रकार छोटी नेकियों का भी अपनी जगह बड़ा महत्व है। इनकी उपेक्षा उचित न होगी। कुछ नेक काम देखने में छोटे होते हैं किन्तु वे नैतिकता और चरित्र की महानता के प्रमाण होते हैं। इसलिए उनकी ओर से बेपरवाह नहीं होना चाहिए। एक बहते हुए तिनके का भी महत्व है। इसके द्वारा हमें नदी के बहाव की दिशा ज्ञात होती है। हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम नेकी और भलाई से सम्बन्ध रखनेवाली किसी चीज़ को भी तुच्छ न समझो, और यह भी एक नेकी है कि तुम अपने भाई से प्रसन्न मुद्रा में मिलो और यह भी (नेकी है) कि तुम अपने डोल से अपने भाई के बरतन में पानी डाल दो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
सच्चाई और परहेज़गारी
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब चार बातें तुममें मौजूद हों तो दुनिया के तुमसे जाते रहने में तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं— अमानत की सुरक्षा, बातचीत में सच्चाई, अच्छी नैतिकता और खाने में सावधानी एवं परहेज़गारी।" (हदीस : अहमद, बैहक़ी फ़ी शोअबुल ईमान)
व्याख्या : 'अमानत' अर्थ की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत पारिभाषिक शब्द है। ईश्वर और उसके बन्दों का हक़ अदा करना, वचन और प्रतिज्ञा का ध्यान रखना, किसी का राज़ मालूम हो तो राज़दारी का पूरा ख़याल रखना, ये सब चीज़ें अमानत के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हैं।
हदीस का अभिप्राय यह है कि दुनिया में यदि किसी को धन की प्रचुरता, सुख-सुविधा और वैभव और पद-प्रतिष्ठा प्राप्त न हो तो कोई हर्ज नहीं। शर्त यह है कि मूलतः जो चीज़ अपेक्षित है वह उसे प्राप्त हो। यदि अभीष्ट चीज़ प्राप्त है तो दुख और परेशानी की कोई बात नहीं। जीवन में वास्तव में जो चीज़ अभीष्ट है वह कोई बाह्य वस्तु नहीं है बल्कि वह आदमी स्वयं है। यदि स्वयं को तबाह होने से उसने बचा लिया है तो दुनिया के छिन जाने पर उसे कोई दुख और अफ़सोस नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अगर उसे वह सब कुछ मिल जाए जिसकी दुनियापरस्त इनसान इच्छा रखता है, चाहे वह स्वयं तबाह हो जाए, तो यह कोई लाभ का सौदा न होगा। हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) का कथन है—
“यदि मनुष्य सारे जगत् को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा।" (मरक़ुस, 8:36)
इनसान वास्तव में एक नैतिक अस्तित्व है। यदि नैतिक दृष्टि से वह अपना मूल्य खो देता है तो उसके लिए इससे बढ़कर और तबाही नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति मृत समान है। उसकी सांसारिक सुख सामग्री के कारण उसपर रश्क करना और उसके सदृश होने की कामना करना बेख़बरी के अतिरिक्त कुछ नहीं। नैतिक दृष्टि से आदमी जीवित है या मृत इसका अनुमान उसके दैनिक जीवन को देखकर किया जा सकता है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने चार चीज़ों का उल्लेख किया है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि आदमी को यदि अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है तो समझना चाहिए कि वह जीवित है, नैतिक रूप से मृत नहीं है।
यदि आदमी को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो उससे किसी अमानत की सुरक्षा सम्भव नहीं है। अमानत का रक्षक वही व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर और उसके बन्दों के हक़ों को पहचानता और उनको अदा करने की चिन्ता करता हो, जिसकी ज़बान सदैव सच्चाई के लिए खुलती हो, जो सुशील हो। खाने-पीने के मामले में जिसमें साधारणतः लोग असावधान होते हैं, वह अत्यन्त सजग हो। हराम और सन्दिग्ध चीज़ों के निकट न फटकता हो। खाने में आवश्यकता की सीमा का भी वह पूरा लिहाज़ करता हो, ऐसा नहीं कि वह पेट ही का बन्दा बनकर रह गया हो।
(2) हज़रत इमरान-बिन-हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर उस मोमिन बन्दे से प्रेम करता है जो निर्धन होने के बावजूद स्वाभिमानी हो, यद्यपि वह बाल-बच्चोंवाला ही क्यों न हो।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : स्वाभिमानी होने का अभिप्राय यह है कि आदमी नाजाइज़ तरीक़े से आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास न करे और किसी के सामने अपनी आवश्यकताएँ प्रदर्शित करने से भी बचे। यदि कोई मोमिन व्यक्ति निर्धन है और उसके बाल-बच्चे भी हैं, फिर भी वह अपनी मर्यादा और अपने स्वाभिमान का लिहाज़ रखता है तो निश्चय ही वह ईश्वर का प्रिय बन्दा है। ईश्वर उसे विशेष प्रेम की दृष्टि से देखता है। यदि बन्दे को इसका एहसास हो तो भूखे रहने के कष्ट में भी उसे आनन्द की अनुभूति होगी।
इस्लाम एक ओर परहेज़गारी और स्वाभिमान पर बल देता है, दूसरी ओर वह इस बात की शिक्षा देता है कि समाज के ऐसे लोगों को उनके हाल पर न छोड़ा जाए बल्कि यथासम्भव अच्छे तरीक़े से उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने की कोशिश की जाए। क़ुरआन में है—
“जो लोग अपने माल को रात-दिन छिपे और खुले ख़र्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके 'रब' के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे।" (2:274)
रात और दिन के मुक़ाबले में छिपे और खुले के उल्लेख में जो साहित्यिक गुण पाया जाता है, वह साहित्य प्रेमियों से छिपा नहीं है। छिपे रूप में इसलिए ख़र्च किया जाए कि ज़रूरतमन्दों की ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और किसी को पता भी न चले। इस प्रकार मुहताजों का स्वाभिमान भी आहत न होगा और उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो सकेगी।
(3) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझे बुलाया और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझपर यह शर्त लगा दी कि किसी इनसान से कुछ भी न माँगना। मैंने कहा कि मुझे स्वीकार है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“और अपना कोड़ा भी न माँगना यदि वह तुमसे छूटकर गिर पड़े, यहाँ तक कि स्वयं ही (सवारी से) उतरकर उठा लेना।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : माँगना चाहे किसी तरह का हो, इससे बचना ही अच्छा है। माँगने और सवाल करने की नहीं, बल्कि न माँगने और सवाल न करने की नीति ईश्वर को प्रिय है। घोड़े पर से उतर कर अपना गिरा हुआ कोड़ा ले लेना तुम्हारे लिए इससे अधिक सुगम हो कि तुम उसके लिए किसी से सवाल करके उसके आभारी बनो।
एहतियात और सावधानी
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में से एक की मृत्यु हुई तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें जन्नत की ख़ुशख़बरी हो। इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तू यह बात कहता है। शायद वस्तुस्थिति से तू अवगत नहीं। सम्भव है उसने कोई व्यर्थ बात की हो या ऐसी चीज़ में कृपणता दिखाई हो जिसमें उसके लिए हानि और किसी कमी की आशंका न थी।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मतलब यह है कि किसी मृत व्यक्ति के विषय में पूरे विश्वास के साथ यह कहना कि वह जन्नती है, एहतियात के विरुद्ध और एक प्रकार से परोक्ष के ज्ञान का दावा करना है। इससे बचना आवश्यक है। वास्तविकता का ज्ञान ईश्वर के सिवा किसी को नहीं हो सकता। किसी को क्या पता कि जन्नत में प्रवेश पाने में उन कर्मों के कारण भी रुकावट पैदा हो सकती है, जिनको सामान्यतः लोग अधिक महत्व नहीं देते। उदाहरण के रूप में दो बातों का उल्लेख किया। आदमी में यदि दूसरी कोई बुराई नहीं है परन्तु यदि उसने व्यर्थ बातों अर्थात् अपनी बातचीत में उन बातों से परहेज़ नहीं किया जो न उसके लिए आवश्यक थीं और न उन बातों में उसका कोई फ़ायदा ही था तो यह चीज़ भी उस व्यक्तित्व के लिए किसी बदनुमा दाग़ से कम नहीं जिसके कारण उसके जन्नत में प्रवेश करने में विलम्ब भी हो सकता है। इसी प्रकार यह चीज़ भी जन्नत में प्रवेश करने में रुकावट बन सकती है कि कोई कृपणता से काम लेता रहा हो, यद्यपि मोमिन के लिए कृपणता से काम लेने का कोई औचित्य नहीं है। मोमिन पर जो सदक़े अनिवार्य हैं उनको अदा करने में उसके लिए बरकत है। नेक कामों में अपना माल ख़र्च करके आदमी अपने को हानि कदापि नहीं पहुँचाता। क़ुरआन में है—
“और तुम जो कुछ ख़र्च करो उसकी जगह वह तुमको और देगा। वह उत्तम दाता है।" (34:29)
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का भी कथन है—
“और सदक़े से माल कम नहीं होता।" (हदीस : मुस्लिम)
अब यदि किसी ने अपने जीवन में कंजूसी दिखाई तो यह चीज़ भी जन्नत के प्रवेश में एक रुकावट बन सकती है। कुछ लोग ऐसी चीज़ों में भी कृपणता से काम लेते हैं जिनमें यदि वे उदारता से काम लें तो उनका कोई नुक़सान नहीं। यह ऐसी बात है जिसे हर कोई समझ सकता है। उदाहरण के रूप में किसी ज़रूरतमन्द को पानी या नमक आदि दे देना या किसी को सलाम करना आदि। ईश्वर के यहाँ इस कृपणता पर पकड़ हो सकती है और इसके कारण जन्नत में प्रवेश पाने में विलम्ब या रुकावट की आशंका हो सकती है।
(2) हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-अबी-बकर अपने पिता के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने एक व्यक्ति की प्रशंसा की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तूने उसकी गरदन काटी।" यह आपने तीन बार कहा। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "जब तुममें से कोई आवश्यकतावश अपने साथी की प्रशंसा करे तो इस सिलसिले में जो कुछ वह कहना चाहता हो उसके विषय में यूँ कहे कि मैं उसे ऐसा समझता हूँ, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में भी वह अच्छा और उत्तम व्यक्ति है, मैं यह नहीं कहता।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से इस बात का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि अपनी बातचीत में आदमी को कितनी सतर्कता से काम लेना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रशंसा उसके लिए घातक भी हो सकती है। इसी को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) गरदन काटना कह रहे हैं। प्रशंसा करने से इस बात की अधिक आशंका होती है कि कहीं इससे आदमी के अन्दर अहंकार और घमन्ड न उत्पन्न हो जाए। यह चीज़ उस व्यक्ति के लिए किसी विनाश से कम नहीं होती। किसी की प्रशंसा करना आवश्यक हो तो उसके साथ इस बात को भी प्रकट करे कि वास्तविकता का ज्ञान सिर्फ़ ईश्वर को है। कौन कैसा है और कैसा नहीं, यह वही जान सकता है।
(3) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो कोई अपने भाई की सिफ़ारिश करे, फिर वह उसके बदले में उसके यहाँ उपहार भेजे और वह उसे स्वीकार कर ले तो निश्चय ही वह ब्याज के द्वारों में से एक बड़े द्वार में प्रवेश कर गया।" (हदीस-अबू-दाऊद)
व्याख्या : ब्याज अपनी मूल आत्मा की दृष्टि से यही तो है कि हम ऐसे तरीक़े से फ़ायदा उठाने का प्रयास करें जिससे इनसानी सहानुभूति और हितैषिता की भावना को आघात पहुँचता है। दूसरे शब्दों में किसी की विवशता को हम शोषण का माध्यम बनाएँ, यह नीति दान, सदक़ा और दानशीलता के सर्वथा विरुद्ध है। सिफ़ारिश के बदले में उपहार स्वीकार करके यदि फ़ायदा उठाते हैं, तो वस्तुतः हम अपने इस अमल से उस मानसिकता का पोषण करते और शक्ति पहुँचाते हैं जो मानसिकता एक सूदख़ोर व्यक्ति की होती है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शब्दों में, ऐसा करके हम ब्याज के द्वारों में से एक बड़ा द्वार खोल रहे होते हैं। और इस प्रकार उस द्वार को बन्द कर रहे होते हैं जो त्याग, क़ुरबानी और जनसेवा का द्वार है, हालाँकि मोमिन का कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी द्वारों को बन्द करने का प्रयास करे जिससे समाज में किसी ख़राबी के पैदा होने की आशंका होती हो।
(4) हज़रत औफ़-इब्ने मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दो आदमियों के बीच किसी मामले का फ़ैसला किया तो जो व्यक्ति मुक़द्दमा हार गया, वह जब पीठ फैरकर लौटा तो उसने कहा— मेरे लिए ईश्वर पर्याप्त है और वह अच्छा कार्यसाधक है। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर साहसहीनता और मूर्खता पर मलामत करता है अपितु तुम्हारे लिए जागरूकता और होशियारी आवश्यक है। फिर यदि (किसी कारण) तुम हार जाओ, उस समय तुम कहो कि मेरे लिए ईश्वर पर्याप्त है और वह अच्छा कार्यसाधक है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि किसी भी मामले के लिए होशियारी और उपाय करना आवश्यक है। यह सही नहीं है कि थककर बैठ रहे, आलस से काम ले और बुद्धिमत्ता और होशियारी के साथ उसके लिए प्रयास ही न करे, फिर जब मुसीबत सिर पर आए तो अपने आपको अनुचित रूप से सांत्वना देने लगे।
(5) हज़रत ज़ैनब बिन्ते-अबी-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम बर्रा (आज्ञाकारी स्त्री) रखा गया तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम अपनी उत्कृष्टता का दावा न करो। तुममें जो नेक काम करनेवाले हैं उन्हें ईश्वर भली-भाँति जानता है। तुम इसका नाम ज़ैनब रख दो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : स्वयं अपनी उत्कृष्टता का दावा करना एहतियात के ख़िलाफ़ है। इसका सही ज्ञान ईश्वर ही को है कि कौन व्यक्ति कैसा है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसे नाम भी बदल दिए हैं जो मानवीय गरिमा और सम्मान के विरुद्ध थे। अतएव सहीह मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की एक बेटी का नाम आसिया (गुनाहगार) था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसका नाम बदलकर जमीला रखा। बुरे और ऐसे नाम जो बहुदेववाद के पोषक हों नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कदापि शेष न रहने देते थे। ज़ैनब एक सुगन्धित और सुन्दर वृक्ष को कहते हैं।
ईश-भय या ईश-परायणता
(1) हज़रत अबू-ज़र ग़िफ़ारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा—
"तुम न किसी गोरे के मुक़ाबले में अच्छे हो और न किसी काले के मुक़ाबले में, यह और बात है कि ईश-परायणता के कारण तुम्हें किसी पर श्रेष्ठता प्राप्त हो।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठता का मौलिक मानदण्ड ईश-भय और तक़वा है, न कि कोई दूसरी चीज़। क़ुरआन में भी कहा गया है—
“वास्तव में ईश्वर के यहाँ तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक (अल्लाह का) डर रखता है।” (49:13)
दिल में ईश्वर का भय हो और जीवन का निर्माण ईश-भय ने किया हो, बस यही चीज़ आदमी को श्रेष्ठ बनाती है। माल, दौलत, रंग, नस्ल, भाषा, राष्ट्र और क्षेत्र के आधार पर किसी को श्रेष्ठ समझना मात्र अज्ञान और गुमराही है। इस अज्ञान ने दुनिया में जो फ़साद और बिगाड़ पैदा कर दिया है उससे प्रत्येक दृष्टिवान अवगत है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि किस चीज़ के कारण अधिकतर लोग नरक में जाएँगे? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "मुँह और शर्मगाह के कारण।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से यह भी पूछा गया कि किस चीज़ के कारण अधिकतर लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ईश-परायणता और सुशीलता के कारण।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इनसान की ज़बान और उसकी बातचीत से यह पता चलता है कि उसका स्वभाव और चरित्र कैसा है और वह किस कोटि का व्यक्ति है। आदमी यदि पतित मानसिकता का है तो यह मानसिकता उसकी बातचीत से प्रकट होकर रहेगी। इसके विपरीत आदमी यदि उच्च कोटि का है तो अनिवार्यतः उसकी ज़बान भी उसकी उच्चता का पता देगी।
इनसान के अन्दर यौन प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इनसान का व्यक्तित्व आहत न हो इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य का अपनी यौन प्रवृत्ति पर पूरा नियन्त्रण हो जिससे वह ग़लत राह पर चलने से बच सके।
ज़बान और यौन-प्रवृत्ति को हम इनसान की दो कमज़ोरियों के रूप में देखते हैं। इनपर नियन्त्रण रखना आवश्यक है, लेकिन इनपर सीधे नियन्त्रण पाना कठिन है। इसलिए आवश्यक है कि इनसान अच्छी सोच और अभिरुचिवाला हो और उसके समक्ष जीवन का कोई उच्च उद्देश्य हो। इस स्थिति में हम यह आशा कर सकते हैं कि वह सामयिक भावनाओं एवं आवेगों में बह जाने से बच सकता है।
वासनाओं और ज़बान पर नियन्त्रण न होने के कारण यही नहीं कि आदमी अपना महत्व एवं मूल्य खो देता है और उसका परलोक बिगड़ जाता है, बल्कि दुनिया में भी मानव समाज को बिखराव, अत्याचार, हिंसा और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मानव समाज से सुख-शान्ति सदैव के लिए विदा हो जाती है।
ईश-भय और नैतिकता में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। नैतिकता जीवन का मूलधन और जीवन का सौन्दर्य है। ईश परायणता एवं कर्तव्यबोध वह शक्ति है जिससे आदमी की नैतिकता और उसके चरित्र में सुदृढ़ता आती है। ईश परायणता और नैतिकता दो ऐसे मौलिक गुण हैं जिनसे भलाई और कल्याण के द्वार खुलते हैं और नेकियों को बढ़ावा मिलता है। ईश परायणता और नैतिकता के द्वारा जीवन के लिए अपेक्षित सारे गुण आदमी में एकत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर अनिवार्यतः उस स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिसका उसने अपने नेक बन्दों से वादा कर रखा है।
(3) हज़रत समुरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"कुलीनता की हैसियत माल की है और श्रेष्ठता ईश-परायणता पर निर्भर करती है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मात्र माल और दौलत के कारण कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जो चीज़ किसी आदमी को श्रेष्ठता प्रदान करती है, वह ईश परायणता का गुण है। यदि किसी में ईश परायणता नहीं है तो मात्र कुलीनता के द्वारा वह श्रेष्ठता के दर्जे को प्राप्त नहीं कर सकता।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा, मैं यात्रा करना चाहता हूँ, आप मुझे नसीहत करें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने ऊपर ईश-परायणता को अनिवार्य कर लो और हर ऊँचे स्थान पर 'तकबीर कहो।' फिर जब वह व्यक्ति वापस जाने लगा तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “ऐ अल्लाह! इसके लिए यात्रा की दीर्घता को लपेट दे और इस यात्रा को इसके लिए सुगम कर दे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ईश-परायणता वस्तुतः होशमन्दी और ईश-भय का नाम है। ईश-भय जीवन के निर्माण का वास्तविक आधार है। जीवन निर्माण के लिए यह आधार प्राप्त न हो सके तो जीवन गरिमाहीन और तिरस्कृत होकर रह जाएगा और उसका दारिद्रय दूर न होगा। केवल यही नहीं कि जीवन प्रतिष्ठारहित हो जाएगा, बल्कि जीवन में कुछ ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएँगी, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति महसूस करेगा। बेईमानी, अत्याचार, निर्दयता और अन्याय आदि वास्तव में ईश्वर से न डरने के कड़वे-कसैले फल हैं, जिनकी कड़वाहट को सभी महसूस कर रहे हैं।
जीवन को सँवारने और उसे महत्वपूर्ण बनानेवाली चीज़ ईश्वर का डर है। उर्वर भूमि भी उस समय तक बेकार है जब तक उसमें खेती न की जाए। भूमि में बीज पड़ने के पश्चात् ही उसकी उर्वराशक्ति का प्रदर्शन होता है और उसकी उर्वराशक्ति को हम एक लहलहाती हरी-भरी फ़सल के रूप में देखने लगते हैं। ईश्वर का डर वह बीज है जो जीवन की फ़सल के लिए दरकार है। इस बीज के प्राप्त न होने की स्थिति में झाड़-झंकाड़ के सिवाए हम किसी अच्छी फ़सल की आशा नहीं कर सकते।
उच्च स्थान पर तकबीर अर्थात् अल्लाहु अकबर (ईश्वर सबसे बड़ा है) कहो। तुम्हें ऊँचाई पर ईश्वर की बड़ाई का ख़्याल हो। इससे ज्ञात हुआ कि यह जीवन यात्रा का सौन्दर्य है कि दुनिया की हर चीज़ विभिन्न प्रकार से हमें ईश्वर का स्मरण कराए। कितनी आकर्षक है जीवन की यह यात्रा! और कितनी भाव विभोर कर देनेवाली हैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाएँ।
(5) हज़रत अली इब्ने-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन के अन्तिम शब्द ये थे—
“नमाज़-नमाज़, और जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं उनके सम्बन्ध में ईश्वर से डरते रहना।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जीवन के अन्तिम क्षण तक अपनी उन ज़िम्मेदारियों का कितना एहसास था जो एक आह्वानकर्ता और उपदेशक के रूप में आपपर थीं। दुनिया से प्रस्थान करते हुए भी आप अपने कर्तव्यों के निर्वाह की ओर से ग़ाफ़िल न हुए और ताकीद की कि तुम न तो ईश्वर के हक़ से ग़ाफ़िल होना और न ही बन्दों के हक़ की ओर से ग़ाफ़िल होना। ईश्वर के बन्दों में लौंडी और ग़ुलाम आदि अधीनस्थ होने के कारण इसके ज़्यादा हकदार हैं कि हम उनका ध्यान रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसी लिए उनका उल्लेख किया और इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि जो तुम्हारे अधीनस्थ हों तुम उनके सम्बन्ध में कदापि उपेक्षा की नीति न अपनाना। यदि उनके साथ किसी प्रकार की ज़्यादती और अत्याचार हुआ तो इसपर ईश्वर की सख़्त पकड़ होगी।
एक हदीस में है कि एक औरत को एक बिल्ली के कारण यातना दी गई जिसको उसने बाँध रखा था, यहाँ तक कि वह भूखी मर गई। वह न तो उसे खाने को देती थी और न उसे छोड़ती ही थी कि वह स्वयं कुछ शिकार करके खा लेती।
जिस ईश्वर ने बिल्ली के उत्पीड़न और उसकी तकलीफ़ों की उपेक्षा नहीं की और उस औरत को अपने किए का मज़ा चखना पड़ा, वह ईश्वर पीड़ित इनसानों की आह को कैसे नज़रअन्दाज़ कर सकता है। इसी लिए कहा कि अधीनस्थों के विषय में ईश्वर से डरो। यदि किसी इनसान का मौलिक स्वभाव विकृत हो गया है और उसे मजबूरों और असहायों की तकलीफ़ों का कुछ एहसास नहीं होता तो कम-से-कम उसे अपनी उस तकलीफ़ का तो एहसास करना चाहिए जब ईश्वर उसके ज़ुल्म और अत्याचार के बदले में उसे कठोर दण्ड देगा और उसको अपनी रहमतों से वंचित कर देगा।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी अन्तिम वसीयत में सबसे अधिक नमाज़ की ताकीद की। नमाज़ के महत्व को देखते हुए इसे दोहराया। नमाज़ ईश्वर का हक़ भी है जो बन्दे पर क़ायम होता है। इसके अतिरिक्त इनसान के लिए नमाज़ एक बड़ी नेमत है और उसके लिए श्रेयस्कर भी है। नमाज़ इतनी विशिष्टताओं वाली इबादत है कि उसके गुणों की गणना सुगम कार्य नहीं है। क़ुरआन और हदीसों की रौशनी में आप जितना अधिक विचार करेंगे, नमाज़ का महत्व और मूल्य बढ़ता ही चला जाएगा। हम यहाँ उसके एक पहलू का उल्लेख करना चाहेंगे।
नमाज़ आदमी में यह विशेष गुण पैदा करना चाहती है कि वह सदैव और प्रतिक्षण ईश्वर को अपने समक्ष करने लग जाए। ईश्वर को अपने से क़रीब पाने और महसूस करने से बढ़कर जीवन की दूसरी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और न इससे बढ़कर मानव जीवन को गरिमावान और मूल्यवान बनानेवाली कोई चीज़ हो सकती है। यह एक ऐसा धन है जिसके सामने दुनिया के सारे धन तुच्छ हैं। यह एक ऐसी आनन्ददायक चीज़ है जिसके मुक़ाबले में दुनिया के सारे आस्वाद फीके पड़ जाते हैं। इस बड़ी नेमत को पाने के पश्चात् केवल यही नहीं कि इनसान के मन-मस्तिष्क और हृदय सँवर जाते हैं अपितु वह महसूस करने लगता है कि इस नेमत के बिना जीवन तो एक सुनसान खण्डहर है, जिसमें भयावहता के अतिरिक्त कुछ न हो।
नमाज़ का यह पहलू बहुत स्पष्ट है कि वह हमें उस स्थान तक ले जाना चाहती है कि हम ईश्वर को अपने समक्ष पाएँ। इस सिलसिले में यहाँ कुछ हदीसों का उल्लेख किया जा रहा है—
एक हदीस में आदमी को नमाज़ में अपने सामने थूकने से मना किया गया है, क्योंकि उसके सामने ईश्वर का रुख़ होता है। एक हदीस में है कि जब तक नमाज़ी नमाज़ की हालत में है और इधर-उधर नहीं देखता, ईश्वर का रुख़ उसके सामने रहता है और जब वह इधर-उधर देखने लगता है तो ईश्वर अपना रुख़ उसकी ओर से फेर लेता है। इसकी पुष्टि उस हदीस से भी होती है जिसमें आया है कि नमाज़ की हालत में बन्दा जो ईश्वर की प्रशंसा, गुणगान और विनती करता है, ईश्वर उसका उत्तर देता है।
एक हदीस से ज्ञात होता है कि नमाज़ बन्दे का अपने प्रभु से मिलन है। मिलन में मनुष्य उससे निकट होता है जिससे वह मिल रहा होता है। मिलन का एक पहलू यह भी है कि दोनों एक-दूसरे की ओर उन्मुख होते हैं और परस्पर बातचीत करते हैं। नमाज़ में मुलाक़ात की ये सारी ही बातें पाई जाती हैं। केवल एक बात कही जा सकती है वह यह है कि मुलाक़ात में आदमी उसको अपनी आँखों से देखता भी है जिससे वह मुलाक़ात करता है। पहली बात तो यह है कि मुलाक़ात के लिए देखना आवश्यक नहीं है। एक अन्धा व्यक्ति भी मुलाक़ात करता है। मात्र इसलिए कि वह अन्धा है हम यह नहीं कह सकते कि उसने मुलाक़ात नहीं की। फिर यह बात भी है कि मोमिन ईश्वर को आँख से न सही दिल की आँख से तो देखता ही है। क़ुरआन में है—
“निगाहें उसे नहीं पा सकतीं लेकिन वह निगाहों को पा लेता है, वह अति सूक्ष्मदर्शी और ख़बर रखनेवाला है।" (6:103)
इस आयत में ईश्वर ने अपने विशेष गुण का उल्लेख किया है कि वह उन मूर्तिमान चीज़ों की भाँति नहीं है जो आँखों को दिखाई देती हैं। वृक्ष, भवन आदि को आँख देखती है, लेकिन ये वृक्ष और भवन आँख को नहीं देखते। देख सकने का गुण उनमें नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के मुक़ाबले में आँख उस निर्जीव पत्थर के सदृश है, जिसका किसी चीज़ को देख न पाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह चीज़ सिरे से है ही नहीं। ईश्वर हमारी आँखों को देखता है। दृष्टि मूलतः यहाँ नहीं वहाँ है। हमारी आँख में तो यह शक्ति भी नहीं है कि हमारी आत्मा का प्रतिबिम्ब उसपर पड़ सके और हम आत्मा को आँख से देख सकें। लेकिन हमारे भीतर एक शक्ति और भी है। वह चेतना और प्रज्ञा की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा आदमी को अपनी आत्मा की अनुभूति होती है और वह समझता है कि यह शारीरिक अस्तित्व उसके मुक़ाबले में निम्नतर है। प्रज्ञा शक्ति के द्वारा उस ईश्वर के अस्तित्व की परानुभूति भी मानव कर सकता है जिसकी सत्ता और गुणों की प्रतिच्छाया चतुर्दिक दिखाई देती है। स्वयं हमारी आत्मा भी उसकी एक प्रतिच्छाया है। हमारी आत्मा जितना अपना पता देती है उससे कहीं बढ़कर अपने प्रभु की सूचना देती है।
ईश्वर और बन्दे के बीच यदि कोई चीज़ रुकावट है तो स्वयं बन्दे की अपनी यह कमज़ोरी है कि वह किसी दूसरे की ओर आकृष्ट होता है। नमाज़ में चूँकि सारे सम्बन्धों से अलग होकर बन्दा ईश्वर के आगे खड़ा होता है इसीलिए अब वह ईश्वर के सामने है, बीच में कोई रुकावट और दूरी नहीं है। हदीस में आता है कि मरनेवाला क़ब्र में ईश्वर से मुलाक़ात करता है, तो इसका अर्थ भी यही है कि वहाँ अन्य सारी रुकावटें समाप्त हो चुकी होती हैं, क्योंकि ईश्वर और बन्दे के बीच कोई रोक नहीं होती।
अल्लाह और बन्दे के बीच अस्ल रुकावट का सम्बन्ध मानसिकता और नैतिकता से है। स्थानगत और कालगत दूरी तो यहाँ पाई नहीं जाती। जितनी भी रुकावटें हैं उनका सम्बन्ध हमारी ग़फ़लत से है। यही कारण है कि हदीस में आता है कि नमाज़ की हालत में छींक, जमाई, ऊँघ आना, हैज़ (मासिक धर्म), क़ै और नकसीर शैतान की ओर से है। ऐसा इसलिए कहा गया कि इन चीज़ों से नमाज़ में व्यवधान उत्पन्न होता है। तहज्जुद की नमाज़ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अधिक एकाग्रता पाई जाती है। संसार और संसार की चीज़ों से अलग होकर बन्दा अपने ईश्वर के समक्ष खड़ा होता है। इसी लिए हदीस में आया है—
“ईश्वर बन्दे से सबसे अधिक निकट रात के अन्तिम पहर में होता है।"
रात में क़ियाम अर्थात् नमाज़ में खड़े होने के विषय में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन भी है—
“वह तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रभु का सामीप्य है और बुराइयों को मिटानेवाला एवं गुनाहों से रोकनेवाला है।"
नमाज़ ईश्वर की महानता और उसके प्रति प्रेम का सिक्का हृदयों में बैठाती है। नमाज़ के द्वारा आदमी के भीतर यह गुण पैदा हो जाता है कि उसके अन्दर ईश्वर के उससे दूर न रहने का एहसास सदैव शेष और जीवन्त रह सकता है। उसका सदैव और प्रतिक्षण जिससे मामला पेश आता है, वह कोई और नहीं ईश्वर ही की सत्ता है।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“परस्पर एक-दूसरे से ईर्ष्या न करो। परस्पर एक-दूसरे की खोद-कुरेद में न पड़ो। एक-दूसरे से द्वेष न रखो। शत्रुता न करो। तुममें से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा न करे। ईश्वर के बन्दे और भाई-भाई बन जाओ। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, वह न उस पर ज़ुल्म करे और न उसे असहाय छोड़े और न उसे तुच्छ समझे। तक़वा (ईशभय) यहाँ है।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार अपने सीने की ओर संकेत करते हुए कहा। “इनसान के लिए यही बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को तुच्छ समझे। मुसलमान पर प्रत्येक मुसलमान की ये चीज़ें हराम हैं : उसका ख़ून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि तक़वा (ईशपरायणता) का मूल केन्द्र इनसान का हृदय है। हृदय में यदि ईश्वर का भय और अपने दायित्व का एहसास पाया जाता है, तो इसका प्रभाव इनसान के पूरे जीवन में दिखाई देगा। जीवन में यदि कोई शुभ परिवर्तन का इच्छुक हो तो उसे यह बात आरम्भ ही में जान लेनी चाहिए कि परिवर्तन उसी समय सम्भव है जब उसके हृदय की दशा ठीक हो, और हृदय का ठीक होना तक़वा के बिना सम्भव नहीं। तक़वा हृदय की सभ्यता है। हृदय अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक दशा में रह सके इसके लिए आवश्यक है कि हृदय में तक़वा को स्थान दिया जाए।
इस हदीस में एक मौलिक बात यह बताई गई है कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। इसलिए दो मुसलमानों के बीच चाहे पारिवारिक सम्बन्ध न भी पाया जाता हो लेकिन उनके बीच दीन और ईमान का जो नाता पाया जाता है वह रंग और नस्ल के नाते से कहीं अधिक गहरा और सुदृढ़ नाता और सम्बन्ध है। इसलिए वे परस्पर भाई-भाई हैं। उन्हें अपने भाई का पूरा ख़याल रखना चाहिए। न वे ख़ुद अपने भाई के साथ किसी प्रकार का ज़ुल्म और अत्याचार करें, न अपने भाई को किसी अत्याचारी के हवाले करें। यह भी एक प्रकार से भाई का हक़ मारना है कि कोई अपने भाई को तुच्छ समझे। यदि कोई अपने भाई के साथ कोई ज़ुल्म ज्यादती तो नहीं करता लेकिन उसे तुच्छ समझता है, तो यही एक बुराई उसके चरित्र को दाग़दार करने के लिए काफ़ी है।
(7) हज़रत अबू-ज़र ग़िफ़ारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुझे एक ऐसी आयत मालूम है कि यदि लोग उसे अपना लें तो वही उनके लिए काफ़ी हो। वह आयत है—
“और जो कोई ईश्वर का भय रखेगा उसके लिए वह (परेशानी से) निकलने की राह पैदा कर देगा। और उसे वहाँ से रोज़ी देगा, जिसका उसे गुमान भी न होगा।" (65: 2-3)
(हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, दारमी)
व्याख्या : यह सूरा अत-तलाक़ की मशहूर आयत है। यह आयत बताती है कि तक़वा और ईशभय कोई साधारण गुण नहीं है। तक़वा अपनाने का अर्थ यह है कि बन्दा ईश्वर की महानता और बड़ाई को स्वीकार करता और अपनी इच्छा के मुक़ाबले में ईश्वर की इच्छा को प्रधानता देता है। ईश्वर की रिज़ा और प्रसन्नता की प्राप्ति ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में ईश्वर उसे बेचारगी और असहाय अवस्था में नहीं रहने देगा। वह उसके लिए परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारे की राह अवश्य निकालेगा। यह भी नहीं सोचा जा सकता कि ऐसा व्यक्ति रोज़ी और आजीविका से वंचित रहेगा। ईश्वर उसके लिए रोज़ी और आजीविका का प्रबन्ध ऐसे तरीक़े से कर सकता है कि उसे पहले से उसका कोई गुमान भी न रहा हो। ईश्वर को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। उसपर भरोसा करके कोई व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता।
अमानतदारी और सच्चरित्रता
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने ख़ुतबे (अभिभाषण) में हमें सम्बोधित किया हो और उसमें यह बात न कही हो कि—
"उस व्यक्ति में ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी न हो और उस व्यक्ति का कोई धर्म नहीं जो अपने दिए हुए वचन का पाबन्द न हो।” (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : ईमान लाने का अर्थ केवल यही नहीं होता कि आदमी ने कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लिया है, बल्कि ईमान अपने पूर्ण भाव में इस बात की अपेक्षा करता है कि आदमी उन सभी ज़िम्मेदारियों को अदा करे जो ईमान लाने के पश्चात् स्वाभाविक रूप से उसपर आती हैं। यह उसी समय सम्भव है जबकि किसी के ईमान ने उसे भरोसे के योग्य बना दिया हो। यदि वह इस योग्य नहीं है कि उसपर विश्वास किया जा सके तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अभी ईमान के मूल्य और उसके वास्तविक अर्थ और उसकी प्रकृति को समझा ही नहीं और न वह ईमान का आस्वादन ही कर सका है।
ठीक यही मामला वचन की पाबन्दी का भी है। यदि आदमी वचन का पाबन्द नहीं है और वह जो वचन और प्रतिज्ञा करता है, उसका उसे कोई लिहाज़ नहीं होता, तो उसका कोई चरित्र नहीं। चरित्र से रहित होने का अर्थ यह हुआ कि उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म जब तक आदमी के जीवन में चरित्र के रूप में व्यक्त न हो, हम उसे धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते।
वास्तव में एक मोमिन और दीनदार व्यक्ति वही है जो इस बात से पूरी तरह अवगत हो कि ईश्वर ने उसे जो आन्तरिक और बाह्य योग्यताएँ प्रदान की हैं वे वस्तुतः ईश्वर की अमानत हैं। ईश्वर का उसपर यह हक़ होता है कि वह उन योग्यताओं और क्षमताओं से काम लेकर अपनी विनयशीलता और वफ़ादारी का प्रमाण दे। उसके जीवन से यह पता चलता हो कि वह ईश्वर की महानता को स्वीकार करता है और ईश्वर ही उसका प्रेमपात्र है। यदि ऐसा नहीं है तो वह अमानतदार नहीं, बल्कि एक अपराधी व्यक्ति है। अमानतदार व्यक्ति ईश्वर के साथ ही नहीं, बल्कि उसके बन्दों के साथ भी ख़ियानत नहीं कर सकता। यदि वह किसी के साथ ख़ियानत करता और उसके विश्वास को आहत करता है तो इसका अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि वह अमानतदारी के गुण से सर्वथा वंचित है। ऐसे व्यक्ति से यह आशा करना मूर्खता है कि वह ईश्वर का वफ़ादार होगा। जब उसमें अमानतदारी का गुण पाया ही नहीं जाता, जिसका प्रमाण इनसानों के साथ उसकी बेवफ़ाई से मिलता है, तो किस आधार पर उससे इसकी आशा की जा सकती है कि वह ख़ुदा का वफ़ादार हो सकता है।
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को वचन देकर उसे भंग कर देता है और अपने दिए हुए वचन का कुछ भी आदर नहीं करता तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसे चरित्रबल प्राप्त नहीं, जो किसी व्यक्ति को वचन का पाबन्द बनाता है। यदि किसी में चरित्रबल नहीं है तो यह समझना मूर्खता है कि वह बन्दों का नहीं तो ख़ुदा का वफ़ादार तो हो ही सकता है। चरित्र में दोरंगी सम्भव नहीं, बल्कि चरित्र को चरित्र कहते ही इसलिए हैं कि उसमें बहुरंगी और किसी प्रकार के विरोधाभास की आशंका नहीं पाई जाती। चरित्रवान हर जगह चरित्रवान होगा और चरित्रहीन हर जगह चरित्रहीन दिखाई देगा। यही कारण है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति ईश्वर का भी आभारी नहीं हो सकता जो इनसानों के साथ कृतघ्नता की नीति अपनाता है।"
वचन देने को मूल हदीस में 'अह्द की पाबन्दी' कहा गया है। अमानत और अह्द के अर्थ में बड़ी व्यापकता पाई जाती है। अमानतदार और अह्द का पाबन्द होने के लिए आवश्यक है कि आदमी अपने पूरे जीवन में वह कार्यनीति अपनाए जो ईश्वर और उसके रसूलों के आदेशों के प्रतिकूल न हो। इस्लामी जीवन अपनी मूल आत्मा और वास्तविकता की दृष्टि से अमानतदारी और वचनबद्धता ही का दूसरा नाम है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा कर दो, और जिस किसी ने तुम्हारे साथ ख़ियानत की हो तुम उसके साथ ख़ियानत न करो।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद, दारमी)
व्याख्या : मतलब यह है कि तुम्हारे लिए प्रत्येक दशा में अमानतदारी का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ ख़ियानत ही क्यों न करे, तुम्हें उसके साथ ख़ियानत नहीं करनी है। तुम्हारी नीति लोगों की नीति की पाबन्द न हो कि वे भलाई करें तो तुम भी भलाई करो और यदि वे बुरे हो जाएँ तो तुम भी बुरे बन जाओ। एक अन्य हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“तुम इस नियम की पाबन्दी करो कि यदि लोग नेकी करें तो तुम्हें नेकी तो करनी ही है, और यदि वे दुर्व्यवहार करें तो इस दशा में भी तुम अत्याचार की नीति कदापि न अपनाओ।"
एक और प्रसिद्ध हदीस है, जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है कि मेरे रब ने मुझे नौ बातों का हुक्म दिया है। इनमें से तीन बातें आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ये बताईं कि जो मेरा हक़ मारे मैं उसका हक़ अदा करूँ, जो मुझे वंचित करे मैं उसे प्रदान करूँ और जो मुझपर ज़ुल्म करे मैं उसे क्षमा करूँ।
(3) उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे कहती हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास हिन्द आईं और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अबू-सुफ़ियान कंजूस व्यक्ति हैं, तो क्या इसमें मेरे लिए कुछ हरज है कि मैं बिना उनकी अनुमति के उनके माल में से उनके बाल-बच्चों पर ख़र्च करूँ? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इसमें तुम्हारे लिए कुछ हरज नहीं यदि तुम दस्तूर के अनुसार उनपर ख़र्च करो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि इस्लामी शरीअत की दृष्टि से इस प्रकार दस्तूर के अनुसार ख़र्च करने में कोई हरज नहीं है। इसे न चोरी कहा जाएगा और न दयानतदारी के प्रतिकूल। इस हदीस से यह भी समझा जा सकता है कि ईश्वर ने धर्म को इसलिए नहीं उतारा कि लोगों के लिए कठिनाई और तंगी पैदा की जाए, बल्कि वास्तव में कठिनाई और तंगी दूर करने ही के लिए यह धर्म अवतरित हुआ है।
(4) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब कोई व्यक्ति बात करे और फिर इधर-उधर मुड़कर देखे तो वह अमानत है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यद्यपि उसने ज़बान से यह नहीं कहा कि इसे राज़ रखना लेकिन इधर-उधर उसके मुड़कर देखने का अर्थ यह है कि वह नहीं चाहता कि उसकी बात को लोग जान लें। ऐसी स्थिति में उसकी बात की हैसियत अमानत की है। उसकी इस बात को दूसरे लोगों से बयान करना ख़ियानत है। अब यदि कोई व्यक्ति यह ख़ियानत करता है तो वह ईश्वर के यहाँ इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकता।
(5) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मजलिसों के लिए अमानतदारी आवश्यक है, यद्यपि तीन मजलिसें इससे अलग हैं— वह मजलिस जिसका सम्बन्ध किसी का नाहक़ ख़ून बहाने की साज़िश से हो या वह मजलिस जिसका सम्बन्ध किसी की इज़्ज़त लूटने से हो या वह मजलिस जिसका सम्बन्ध बिना किसी हक़ के किसी का माल छीनने से हो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि किसी मजलिस (सभा) में जो विचार-विमर्श अथवा निर्णय राज़दारी का किया जाए उसकी हैसियत एक अमानत की है। मजलिस के लोगों का यह कर्तव्य होता है कि वे इसे राज़ रखें। किन्तु यदि किसी मजलिस में ज़ुल्म और ज़्यादती जैसे— किसी की इज़्ज़त लूटने या नाहक़ क़त्ल की साज़िश रची जा रही हो तो फिर अमानतदारी इसमें है कि उस योजना को असफल करने का प्रयास किया जाए और उस नापाक साज़िश से उन लोगों को सूचित किया जाए जो उसे असफल करने में प्रभावी क़दम उठाने की स्थिति में हों। ऐसा करना कदापि ख़ियानत नहीं है।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति से परामर्श लिया जाए, इस सम्बन्ध में उसकी हैसियत अमीन (अमानतदार) की होती है।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात् जिस व्यक्ति से सलाह-मशविरा किया जाए, उसे इसका एहसास होना चाहिए कि उसपर भरोसा करके कोई उससे मशविरा कर रहा है। इसलिए वह मशविरा भी सही दे और उसकी बात को भी राज़ में रखे। उसे इधर-उधर लोगों से कहता न फिरे।
(7) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दो हदीसें बयान कीं। इनमें से एक को मैंने देख लिया और दूसरी की प्रतिक्षा कर रहा हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमसे कहा— "अमानत लोगों के दिलों की गहराई में नाज़िल हुई। फिर उन्होंने क़ुरआन को जाना, फिर सुन्नत को जाना।" नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमसे उसके उठ जाने का हाल बयान किया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, आदमी सोएगा और अमानत उसके दिल से क़ब्ज़ (ग्रस्त) कर ली जाएगी। अतः उसका धुँधला-सा प्रभाव रह जाएगा। वह फिर सोएगा तो शेष अमानत भी निकाल ली जाएगी और एक फफोले जैसा निशान रह जाएगा, जैसे आग की कोई चिंगारी तुम अपने पाँव पर डाल दो, और उससे फफोला पड़ जाए, और तुम प्रकट में तो उसे उभरा हुआ देखो, हालाँकि उसमें कोई चीज़ न होगी। हालत यह होगी कि लोग आपस में सौदा करेंगे, किन्तु कोई एक भी अमानत को अदा करता दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि अमुक परिवार में एक अमानतदार व्यक्ति है। और किसी के सम्बन्ध में कहा जाएगा कि वह कितना बुद्धिमान, कितना होशियार और शिष्ट और कितना वीर है। यद्यपि उसके दिल में राई बराबर भी ईमान न होगा। और हमपर एक ऐसा समय बीत चुका है कि किसी के भी हाथ सौदा करने में कुछ परवाह न होती थी। यदि वह मुसलमान होता तो इस्लाम और यदि ईसाई होता तो उसका ज़िम्मेदार उसे मुझपर पलटा देता। किन्तु आज मैं केवल अमुक और अमुक लोगों से ही सौदा करता हूँ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अमानत लोगों के हृदय की गहराई में नाज़िल हुई। अमानत हृदय की प्रकृति है। हृदय की वास्तविक निधि यही है, जिसकी इस हदीस में अमानत से उपमा दी गई है। इसी से हृदय का महत्व और मूल्य है। क़ुरआन में है—
“हमने अमानत को आकाशों, धरती और पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया किन्तु उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए किन्तु मनुष्य ने उसे उठा लिया।” (33:72)
अर्थात् आकाशों, धरती एवं पर्वतों में से किसी में यह सामर्थ्य न थी कि कोई भी इस अमानत को उठा सकता। इस अमानत के उठाने की सामर्थ्य केवल मनुष्य में थी। इसी को यह क्षमता प्रदान की गई कि वह इस अमानत को उठा सके। यह अलग बात है कि कोई व्यक्ति समर्थ होने के बावजूद अमानत में ख़ियानत करे, इसे उसकी सरकशी ही कहा जाएगा।
हदीस में भी है कि ईश्वर कहता है—
“आकाश और धरती में मेरी समाई न हो सकी। मेरी समाई तो मोमिन के दिल में होती है।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर मोमिन के हृदय की परिधि में सीमित होकर रह जाता है, बल्कि इससे अभिप्रेत हृदय की ग्राह्यता है, अर्थात् धरती और आकाश जिन राज़ों के राज़दार नहीं हो सकते, उनका राज़दार मोमिन का हृदय है। मर्मज्ञता तो हृदय का विशेष गुण है। मोमिन के हृदय को ईश्वर का सामीप्य प्राप्त होता है। इस सामीप्य के कारण मोमिन का हृदय उन सभी विशेषताओं और भावों से परिपूर्ण हो जाता है जिनको दीन में मौलिक महत्व प्राप्त है। ज्ञान, परानुभूति, ईशभय, प्रेम, समर्पण, रुजू आदि सभी विशेषताएँ इनसान में पैदा हो जाती हैं। मानव दिव्य-प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, अर्थात वह ईश्वर की छवि और उसके जलवे से आलोकित हो उठता है, जो उसे विश्वास और भरोसे के योग्य बना देता है। फिर वह न तो ईश्वर के साथ विश्वासघात कर सकता है और न ईश्वर के बन्दों को धोखा दे सकता। क़ुरआन में है—
"क्या वह व्यक्ति जो मुर्दा था, हमने उसको जीवन प्रदान किया और उसके लिए रौशनी कर दी, जिसको लिए हुए लोगों के बीच चलता फिरता है।, (क्या वह) उस व्यक्ति की भाँति हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो और उनसे कदापि निकलनेवाला न हो?" (7 : 123)
स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति से इसकी आशंका नहीं हो सकती कि वह किसी मामले में ख़ियानत करेगा। वह किसी को कोई वचन देगा तो उसे अवश्य पूरा करेगा। और यदि किसी व्यक्ति से वह कोई लेन-देन का मामला करेगा तो इसमें सच्चा और खरा सिद्ध होगा। उससे बद-दयानती या किसी प्रकार के विश्वासघात की आशा नहीं की जा सकती।
क़ुरआन और सुन्नत ने भी इस अमानत और इसकी अपेक्षाओं से मनुष्यों को अवगत कराया। मनुष्यों की प्रकृति में जो चीज़ रखी गई थी उससे भिन्न किसी और चीज़ की शिक्षा क़ुरआन और सुन्नत ने मनुष्यों को नहीं दी।
अपनी ग़फ़लत और असावधानी के कारण इनसान अमानत की निधि से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक कि अमानत के प्रभाव भी धीरे-धीरे उसके मन-मस्तिष्क और हृदय से बिलकुल मिट जाएँगे। जिस प्रकार उभरे हुए फफोले में दूषित जल के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उसी प्रकार इनसान नैतिक दृष्टि से बिलकुल खोखला होकर रह जाएगा।
अमानत उठ जाने के कारण लोगों की दशा यह होगी कि वे क्रय-विक्रय और दूसरे मामलों में बेझिझक बद्-दयानती और बेईमानी से काम लेंगे। उन्हें एक-दूसरे के नुक़्सान की कुछ भी परवाह न होगी। शिष्ट से शिष्टतर व्यक्ति को यदि निकट से देखा जाएगा तो ज्ञात होगा कि उसके हृदय में राई के बराबर भी ईमान नहीं है। अमानतदारी और ईमान दोनों अनिवार्यतः एक-दूसरे के पूरक हैं। ईमान के बिना किसी अमानतदारी की आशा नहीं की जा सकती।
इस हदीस में एक ऐसे समय का उल्लेख किया गया है जिसमें मामला चाहे किसी से भी होता, चाहे वह मुसलमान न भी होता, तब भी उससे किसी प्रकार की आशंका नहीं होती थी। दीन और ईमान न सही, अपने सरदारों और ज़िम्मेदारों की पकड़ का ख़्याल उसे विवश करता कि वह हक़ न मारे, बल्कि उसे पूरा-पूरा अदा करे।
हदीस के अन्तिम अंश से यह ज्ञात होता है कि अमानत के उठ जाने की जो सूचना अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दी थी, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के काल ही में उसकी निशानियाँ दिखाई देने लगी थीं।
(8) हज़रत इमरान-इब्ने-हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। उनका बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मेरी उम्मत में सबसे अच्छे मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वे लोग होंगे जो उनके बाद होंगे। फिर वे लोग जो उनके बाद होंगे।" हज़रत इमरान (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने ज़माने के पश्चात् दो ज़मानों को उत्तम ठहराया या तीन को। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “फिर तुम्हारे पश्चात् वे लोग होंगे जो बग़ैर तलब किए ही गवाही देंगे, ख़ियानत करेंगे, अमीन (अमानतदार) न बनाए जाएँगे और वे नज़्र मानेंगे, किन्तु उसे पूरा न करेंगे और उनमें मोटापा ज़ाहिर होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : एक दूसरी हदीस से मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने ज़माने के पश्चात निरन्तर दो ज़मानों को उत्तम ज़माना कहा है। अतएव सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सबसे अच्छे लोग मेरे ज़माने से सम्बन्ध रखते हैं, फिर वे लोग उत्तम हैं जो मेरे ज़माने के लोगों के पश्चात् होंगे, फिर वे लोग जो उनके पश्चात् होंगे। इसके बाद ऐसे लोग होंगे जिनकी गवाही उनकी क़सम के मुक़ाबले में और उनकी क़सम उनकी गवाही के मुक़ाबले में अग्रसरता दिखा रही होगी।"
मतलब यह है कि गवाही देने की लालसा बढ़ी होगी। ज़िम्मेदारी का उन्हें बिलकुल एहसास न होगा।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नुबूवत की घोषणा और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अन्तिम सहाबी के देहान्त के मध्य का ज़माना 120 वर्ष का होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 120 वर्ष की अवधि में दो कालखंड (नुबूवत का ज़माना और सहाबा का ज़माना) व्यतीत हो गए। ताबईन का ज़माना 170 वर्ष में समाप्त हुआ। तबे-ताबईन (जिन्होंने ताबईन को देखा हो) का ज़माना 233 वर्ष (अर्थात 220 हिजरी) में समाप्त होता है। उस समय तक मुस्लिम समुदाय में काफ़ी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी थीं। हदीसों में तीन कालों तक भलाई और कल्याण के प्रभावी रहने की सूचना दी गई है और बताया गया है कि उसके पश्चात् बुराई का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि भलाई दुनिया से एकदम उठ जाएगी। हदीस से मालूम होता है कि प्रत्येक कालखंड में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो सत्य को स्थापित करेंगे और इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे। अधर्मियों का बाहुल्य और उनका प्रभुत्व सत्य मार्ग से उन्हें विचलित न कर सकेगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो अपने ज़माने में ऐसे लोगों का साथ देने का श्रेय प्राप्त करें जो हर प्रकार की गुमराहियों और बिदअतों से दूर रहकर सत्य की स्थापना के लिए संघर्षरत हों।
तौबा और क्षमा याचना
(1) हज़रत अग़र्र मुज़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ लोगो! ईश्वर के समक्ष तौबा करो। मैं दिन में सौ बार उसके समक्ष तौबा करता हूँ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात् मैं स्वयं ईश्वर के समक्ष बार-बार तौबा करता हूँ और उसकी ओर पलटता हूँ, इसलिए तुम भी तौबा को अपने लिए अनिवार्य कर लो।
“मैं सौ बार उससे तौबा करता हूँ" का मतलब यह है कि मैं स्वयं को इसका ज़रूरतमन्द पाता हूँ कि बार-बार ईश्वर की ओर रुख़ करूँ ताकि वह मेरी भूल-चूक को क्षमा कर दे और ईश्वर के सामीप्य के अतिरिक्त मेरा दिल कहीं और चैन न पाए, और इसलिए भी कि ईश्वर के अतिरिक्त मुझे कहीं और आराम नहीं मिलता। इस प्रकार मुझे ईश्वर की विशेष अनुग्रह दृष्टि और अनुकम्पा की भी अधिक से अधिक आशा होती है जिसका एक बन्दा सबसे बढ़कर ज़रूरतमन्द और मुहताज होता है।
तौबा करने का अर्थ है— रुजू करना, लौट आना और झुक जाना। इसी प्रकार एक दशा से दूसरी दशा की ओर रुजू करना भी तौबा है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि पहली दशा बुरी हो, बल्कि अच्छी दशा से उससे उत्तम दशा की ओर रुजू करना भी तौबा है। यह शब्द ईश्वर के लिए भी आता है। उस समय इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर बन्दे पर मेहरबान और उससे राज़ी हो गया। उसने बन्दे की तौबा क़बूल कर ली। उसकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया और उसकी ओर उन्मुख हुआ।
तौबा एक उत्तम और पवित्रतम पारिभाषिक शब्द है। इसमें श्रेष्ठतम पर्दादारी भी पाई जाती है। बन्दा जब घृणित से घृणित कर्म को ईश्वर से डरकर छोड़ देता है और संकल्प करता है कि अब इस कर्म के निकट नहीं जाएगा, तो उसके इस कर्म को स्वीकारोक्ति (Confession) नहीं, बल्कि तौबा का नाम दिया गया, मानो बन्दा अपने ईश्वर की ओर लौटा और उसकी ओर रुजू हुआ है, जो एक उत्तम जीवन-व्यापार है। इस तरह बन्दे के ऐब को छिपाया जाता है, उसे ख़बर दी जाती है कि ईश्वर के यहाँ वह स्वीकृत है और इस प्रकार उसे रुसवाई से बचा लिया जाता है।
(2) हज़रत अग़र्र मुज़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे दिल पर परदा पड़ जाता है, अतः मैं दिन में सौ बार ईश्वर से क्षमा-याचना करता हूँ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हृदय की दशा को कोई क्या बयान कर सकता है। फिर भी हदीस के व्याख्याकारों ने इस हदीस की व्याख्या में अपने कुछ एहसास प्रकट किए हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हृदय की दशा यह थी कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रतिक्षण और प्रत्येक समय अल्लाह को याद करते थे, जैसा कि हदीस में है, “नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रत्येक समय ईश्वर का स्मरण करते थे।" नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते थे कि हृदय सदैव ईश्वर की सेवा में उपस्थित रहे और हुज़ूरी (Presence of God) के एहसास में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, लेकिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ी हुई थीं। बाल-बच्चों के हक़ अदा करने के अतिरिक्त सत्य के आमन्त्रण, जिहाद और लोगों की शिक्षा-दीक्षा आदि कितनी ही ऐसी चीज़ें थीं जिनकी ओर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ध्यान देना पड़ता था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का संवेदनशील हृदय इसे भी एक तरह की ग़फ़लत समझता था और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इसके लिए ईश्वर से क्षमा-याचना करते थे। कुछ व्याख्याकारों की दृष्टि में परदा से अभिप्रेत 'सकीना' है, जो पवित्र हृदय पर उतरता था और उसपर छा जाता था। 'सकीना' से अभिप्रेत दिव्य शान्ति है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क्षमा-याचना वास्तव में आभार प्रदर्शन हेतु और तद्धिक ईश-अनुग्रह के लिए थी, जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है, "क्या मैं कृतज्ञ बन्दा न बनूँ।”
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उस सत्ता की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह न करो तो अनिवार्यतः ईश्वर तुम्हें विनष्ट करके ऐसे लोगों को ले आए जो गुनाह करें और ईश्वर से क्षमा-याचना करें और फिर ईश्वर उन्हें क्षमा कर दे।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि इनसानों को पैदा करने से अभीष्ट यह नहीं है कि उनसे सिरे से कोई गुनाह ही न हो, बल्कि वास्तव में अपराध यह है कि बन्दा अपने गुनाहों पर आग्रह करे। बन्दा अगर ईश्वर के आज्ञापालन में जीवन व्यतीत करता है तो अवश्य ही उसके रब की दृष्टि में इसका महत्व और मूल्य होगा और वह उसकी नेकियों का बदला देगा, और अगर कोई गुनाहों में पड़ जाता है और फिर तौबा करता है और उसकी ओर पलट आता है, तो उसका रब दयावान और क्षमाशील है। वह उसके गुनाहों और ग़लतियों को क्षमा कर देता है।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रत्येक इनसान ख़ताकार है और सबसे अच्छे ख़ताकार तौबा करनेवाले होते हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा, दारमी)
व्याख्या : अर्थात् ख़ता तो इनसान से होती ही है। मानवीय दुर्बलताओं से कौन मुक्त हो सका है। लेकिन सबसे अच्छे लोग वे हैं जो अपनी ग़लतियों पर क़ायम नहीं रहते, बल्कि जल्द से जल्द तौबा करके अपना सुधार कर लेते हैं। वे अज्ञान और अन्धकार में पड़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें वे पड़े नहीं रहते, उससे निकलने का प्रयास करते हैं, उनका सम्बन्ध मूलतः प्रकाश से होता है, अन्धकार से नहीं। वे भलाई से दिलचस्पी रखते हैं, बुराई से उनका सम्बन्ध नहीं होता।
(5) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। उनका बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति इस्तिग़फ़ार (ईश्वर से क्षमा-याचना) को अपने ऊपर अनिवार्य कर ले तो ईश्वर हर तंगी से निकलने की राह उसके लिए पैदा कर देता है और हर रंज और दुख से उसे छुटकारा देता है। और उसे ऐसी जगह और ऐसे तरीक़े से आजीविका प्रदान करता है जिसका उसे अनुमान भी नहीं होता।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद इब्ने-माजा)
व्याख्या : बन्दा प्रत्येक दशा में ईश्वर का मुहताज है। उसपर अनिवार्य है कि इस्तिग़फ़ार के द्वारा अपने प्रभु से जुड़ा रहे। ईश-भय का भी यही अर्थ है। और यही ईश्वर की रहमत को अपनी ओर आकर्षित करने का साधन भी है। क़ुरआन में भी है—
“जो कोई ईश्वर का डर रखेगा उसके लिए वह निकलने की राह पैदा कर देगा और उसे वहाँ से आजीविका देगा जिसका उसे गुमान भी न होगा। जो ईश्वर पर भरोसा करे तो वह उसके लिए काफ़ी है।" (65:2-3)
क़ुरआन के इन शब्दों से हदीस की पुष्टि होती है। इस्तिग़फ़ार के लाभदायक होने की पुष्टि क़ुरआन की इन आयतों से भी होती है।
“और मैंने कहा : अपने रब से क्षमा की प्रार्थना करो। निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील है। वह बादल भेजेगा तुमपर ख़ूब बरसनेवाला और वह माल और बेटों से तुम्हें बढ़ोत्तरी प्रदान करेगा और तुम्हारे लिए बाग़ पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें प्रवाहित करेगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम (अपने दिलों में) ईश्वर के लिए किसी गौरव की आशा नहीं रखते!" (71:10-13)
(6) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर अपने बन्दे की तौबा पर, जब वह (गुनाह के बाद) क्षमा-याचना के लिए उसकी ओर पलटता है, तुममें से उस व्यक्ति से भी अधिक प्रसन्न होता है जिसकी सवारी रेगिस्तान में हो, फिर वह सवारी ग़ायब हो गई और उसी पर उसका खाना-पानी भी था। (उसने इधर-उधर छान मारा किन्तु सवारी न मिल सकी।) अन्ततः वह निराश होकर एक वृक्ष के पास आकर उसकी छाँव में लेट गया। वह उसी हालत में था कि क्या देखता है कि उसकी सवारी (ऊँटनी) उसके पास खड़ी है, उसने उसकी नकेल पकड़ ली और अपार प्रसन्नता के कारण उसकी ज़ुबान से ये शब्द निकल गए कि “ऐ अल्लाह! तू मेरा बन्दा है और मैं तेरा रब हूँ।" यह चूक अपार प्रसन्नता की दशा में उससे हुई (कि ग़लत शब्द उसकी ज़बान से निकल गए।)
व्याख्या : आभार प्रदर्शन के रूप में कहना तो यह चाहिए था कि “ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है और मैं तेरा बन्दा हूँ।” लेकिन अपार प्रसन्नता की दशा में वह कुछ का कुछ कह गया। मतलब यह है कि बन्दे की तौबा से ईश्वर की प्रसन्नता और ख़ुशनूदी हासिल होती है। तौबा करने से पहले बन्दा मानो खो गया था और उसकी तबाही निश्चित हो गई थी। लेकिन तौबा करके उसने अपने जीवित होने का प्रमाण जुटा दिया और अपने को तबाह होने से बचा लिया। ईश्वर चाहता यही है कि उसका कोई भी बन्दा, जिसकी रचना उसने उत्तम प्रकृति के अनुरूप की है, विनष्ट और तबाह न हो।
(7) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह की ओर से, जो अत्यन्त बरकतवाला और उच्च है, जिन बातों का उल्लेख करते थे उनमें से एक उल्लेख यह है कि अल्लाह कहता है, “ऐ मेरे बन्दो! मैंने ज़ुल्म को अपने ऊपर हराम किया है और उसे तुम्हारे मध्य भी हराम किया। अतः तुम आपस में एक-दूसरे पर ज़ुल्म न करो। ऐ मेरे बन्दो! तुममें हरेक गुमराह है सिवाय उसके जिसका मैंने मार्गदर्शन किया। अतः मुझसे मार्गदर्शन चाहो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। ऐ मेरे बन्दो! तुममें से हरेक भूखा है, सिवाय उसके जिसको मैंने खिलाया। अतः तुम मुझसे खाना माँगो, मैं तुम्हें खिलाऊँगा। ऐ मेरे बन्दो! तुममें से हरेक नंगा है, सिवाय उसके जिसको मैंने पहनने को दिया। अतः तुम मुझसे वस्त्र माँगो, मैं तुम्हें पहनाऊँगा। ऐ मेरे बन्दो! तुम रात-दिन ख़ताएँ करते रहते हो और मैं सभी ख़ताओं को माफ़ करता हूँ, अतः मुझसे क्षमा-याचना करो, मैं तुम्हें क्षमादान दूँगा। ऐ मेरे बन्दो! (तुम अगर गुनाह करके) मुझे हानि पहुँचाना चाहोगे तो मुझे कदापि हानि न पहुँचा सकोगे। और अगर नेक काम करके मुझे लाभ पहुँचाना चाहोगे तो कदापि मुझे लाभ न पहुँचा सकोगे। ऐ मेरे बन्दो! यदि तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछले और तुम्हारे मानव और तुम्हारे जिन्न सभी तुम्हारे अपने एक ऐसे व्यक्ति के हृदय के सदृश हो जाएँ जो अत्यन्त ईशपरायण हो, तो इससे मेरी मिल्कियत में कोई अभिवृद्धि न होगी। ऐ मेरे बन्दो! यदि तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछले और तुम्हारे मानव और तुम्हारे जिन्न सभी तुम्हारे अपने एक ऐसे व्यक्ति के हृदय के सदृश हो जाएँ जो अत्यन्त मर्यादाहीन और निकृष्ट हो, तो इससे मेरी मिल्कियत में कोई कमी न होगी। ऐ मेरे बन्दो! अगर तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछले और तुम्हारे मानव और तुम्हारे जिन्न सब के सब एक जगह खड़े होकर मुझसे माँगें और मैं हर इनसान को उसके माँगने के अनुसार दूँ, तो इससे मेरे पास जो कुछ है, उसमें कोई कमी न होगी। होगी तो बस ऐसी ही जैसे किसी समुद्र में किसी सूई के डालने के वक़्त (उस समुद्र के पानी में) होती है। ऐ मेरे बन्दो! ये तो बस तुम्हारे कर्म हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए गिन रखता हूँ, फिर मैं तुमको उन्हें पूरा-पूरा अदा कर दूँगा। अतः जो कोई भलाई पाए उसको चाहिए कि वह ईश्वर की प्रशंसा करे और जो उससे (भलाई से) भिन्न कोई दूसरी चीज़ पाए, वह तो बस अपने आपको मलामत करे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि ईश्वर अगर बन्दे को यूँ ही छोड़ दे और उसके मार्गदर्शन का प्रबन्ध न करे तो वह कदापि मार्ग नहीं पा सकता। वह गुमराही के अंधेरों में भटकता रहेगा और अपनी उस प्रकृति से विलग हो जाएगा जिसका उल्लेख इस हदीस में किया गया है कि "हर बच्चा स्वाभाविक प्रकृति (इस्लाम) पर पैदा होता है।"
एक और हदीस— "तुममें से हर एक गुमराह है सिवाय उसके जिसको मैंने राह दिखाई" के अर्थ को इन शब्दों में बयान करती है—
“निस्संदेह, ईश्वर ने लोगों को अन्धकार में पैदा किया, फिर उनपर अपने प्रकाश की फुहार बरसाई।" इस फुहार ही के द्वारा अन्धकार से छुटकारा सम्भव हो सका। ईश्वर के प्रकाश के मुक़ाबले में जो कुछ है वह अन्धकार है। ईश्वर से अलग होकर इनसान अन्धकार से कदापि नहीं निकल सकता।
ईश्वर के देने से ईश्वर के यहाँ कदापि कोई कमी नहीं होती। इसी को समुद्र और सूई की मिसाल देकर समझाया गया है। मिसालों के द्वारा बात मन में बैठ जाती है और इसे याद रखना भी आसान होता है।
हदीस के अन्तिम शब्द इस हदीस का सार हैं। इनसान को जो और जिस प्रकार की भलाई प्राप्त हो, वह वास्तव में ईश-प्रदत्त है। वह अपने बन्दे को बेइन्तिहा दे सकता है। उसकी क़ुदरत और रहमत अपार है वह स्वयंभू और सारे संसार से निरपेक्ष है लेकिन उसकी दया और दानशीलता से सारा जगत् लाभान्वित हो सकता है। बन्दे के लिए अनिवार्य है कि भलाई में हिस्सा पाकर ईश्वर का कृतज्ञ बन्दा बने और उसकी प्रशंसा करे। और अगर वह भलाई से वंचित रहता है तो इसमें दोष स्वयं बन्दे का है, ईश्वर का नहीं। उसे मलामत करना है तो ख़ुद को मलामत करे। ईश्वर ने तो अपनी रहमत का दरवाज़ा सबके लिए खुला रखा है। अब अगर कोई स्वयं को ईश्वर की रहमत से अलग रखता है तो वह स्वयं अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसी पर आती है।
भय और आशा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो यातना ईश्वर के पास है, अगर ईमानवाले उसे जान लें तो कोई भी उसकी जन्नत का लोभ न कर सके। और जो रहमत ईश्वर के पास है, उसका ज्ञान यदि काफ़िरों को हो जाए तो उनमें से कोई भी उसकी रहमत से निराश न हो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : दुनिया में किसी बन्दे के लिए जो कार्य-पद्धति सही और ठीक हो सकती है, वह यही है कि उसका हृदय न तो ईशभय से रिक्त हो और न वह कभी ईश्वर की रहमत से निराश हो। जीवन को दुरुस्त रखने के लिए भय और आशा दोनों ज़रूरी हैं। भय इनसान को ईश्वर की अवज्ञा से रोकेगा और आशा उसे नेकियों की ओर ले जाएगी।
यह हदीस बताती है कि भय और आशा निराधार नहीं और न ये किसी भ्रम की उपज हैं। ईश्वर के पास ऐसी दर्दनाक यातना तैयार है कि उसकी जानकारी अगर सही तौर पर एक मोमिन बन्दे को हो जाए तो उसकी जन्नत से निराश होकर रह जाए और वह यह समझने लगे कि ईश्वर की इस यातना और उसके प्रकोप से बच निकलना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कुछ ख़बर नहीं कि कौन उसकी लपेट में आ जाए। यातना की प्रचण्डता के मुक़ाबले के लिए हमारे पास जो कर्म और विश्वास की शक्ति है, उसमें वह सामर्थ्य कहाँ कि वह ईश्वर के प्रकोप की प्रचण्डता को कम कर सके।
इसी प्रकार यदि काफ़िर व्यक्ति को, जो किसी तरह भी दया का पात्र नहीं है, ईश्वर की रहमत और उसकी दया का सही ज्ञान हो सके, तो वह भी ईश्वर से आशा करने लग जाएगा और उसे गुमान होगा कि ईश्वर की रहमत जब इतनी व्यापक है और उसमें इतना जोशो-ख़रोश है तो कोई भी जन्नत से वंचित नहीं हो सकता। शायद ईश्वर के प्रकोप और उसकी रहमत का इससे अच्छा चित्रण सम्भव नहीं है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईश्वर के साथ नेक गुमान रखना सबसे अच्छी इबादत है।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ईश्वर के साथ किसी बन्दे का रिश्ता और सम्बन्ध कैसा और किस प्रकार का है इसका अन्दाज़ा आप उस गुमान से कर सकते हैं जो वह अपने रब से रखता है। बन्दे का कर्तव्य है कि वह अपने रब के साथ नेक गुमान रखे। उसके दीन और ईमान का दुरुस्त होना मूलतः इसी पर निर्भर करता है। ईश्वर का मामला अपने बन्दे के साथ उसके गुमान के अनुसार होता है। हदीस में है कि “मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ।" अब यह बन्दे पर है कि वह जैसा चाहे अपने रब के साथ गुमान रखे।
ईश्वर के साथ एक मोमिन व्यक्ति, जो अच्छा गुमान रखता है, उसके कई पहलू हैं—
मोमिन यह समझता है कि उसका रब उसकी ख़बरगीरी से ग़ाफ़िल नहीं हो सकता। इसी लिए उसे अपने रब पर पूरा भरोसा होता है। यही भरोसा दुनिया में उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह जानता है कि ईश्वर ने उसके लिए जो भी फ़ैसला किया है, उसी में उसकी भलाई है। ईश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, वह उसके अतिरिक्त है जिसके योग्य वह वास्तव में था। आख़िरत में भी वह उसके कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देगा।
बिजली, गर्मी, रौशनी आदि से कहीं बढ़कर शक्ति उन कर्मों में पाई जाती है जिनके पीछे सद्भाव और ईश-परायणता क्रियाशील रही हो। यह ईश्वर के प्रति दुराशा होगी कि आदमी हवा, गर्मी, सर्दी आदि के प्रभावों को तो स्वीकार करता हो, लेकिन ईश्वर से निराश हो। नेक कर्मों की उपेक्षा वास्तव में ईश्वर के प्रति सदाशा के विपरीत एक नीति है। क्या नेक कर्मों पर ईश्वर से उसे बदले की आशा नहीं या वह यह सोचता है कि ईश्वर को उसके कर्मों की ख़बर नहीं होती। ईश्वर से अच्छा गुमान एक ऐसी कसौटी है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपने को परखकर देख सकता है कि वह कहाँ खड़ा है और उसने अपने जीवन में ईश्वर को क्या स्थान दे रखा है।
ईश्वर से अच्छा गुमान रखने को इबादत कहा गया है। यह ऐसी इबादत है कि जिसका सिलसिला सदैव क़ायम रहेगा और इस इबादत के साथ दूसरे आवश्यक काम भी किए जा सकते हैं। यह इबादत अन्य कार्यों में रुकावट नहीं बनती। और यह इबादत भी एक बेहतरीन इबादत है।
(3) हज़रत उम्मुल-अला अनसारिया (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे कहती हैं
कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यद्यपि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा और तुम्हारे साथ क्या।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन एक ख़ास घटना से सम्बन्धित है। हज़रत उसमान-इब्ने-मज़ऊन (रज़ियल्लाहु अन्हु), प्रमुख मुहाजिरों में से थे। मुहाजिरों में से सबसे पहले मदीना में उन्हीं की मृत्यु हुई। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनकी मृत्यु के बाद उनके माथे को चूमा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखें नम थीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मौजूदगी में जन्नतुल-बक़ीअ में उनको दफ़न किया गया। एक औरत ने कहा कि “ऐ इब्ने मज़ऊन्! तुझे जन्नत मुबारक हो, तेरी आख़िरत बेहतर है।" इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सचेत करते हुए कहा कि परोक्ष की ख़बर किसी को क्या मालूम। फिर यह अदब के ख़िलाफ़ भी है कि परोक्ष के विषय में कोई बात दृढ़ता और विश्वास के साथ कही जाए। किसका क्या हाल होगा इसे ईश्वर ही जानता है। हदीस के कुछ व्याख्याकारों ने इस बात की सम्भावना व्यक्त की है कि सम्भव है आपने यह बात कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा, उस समय कही हो जब यह आयत न उतरी हो—
"ताकि ईश्वर तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को क्षमा कर दे।" (48:2)
(4)
सुरुचि
अल्लाह की तरफ़ पलटना
(1) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से उल्लेख करते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदम की सन्तान के पास अगर एक घाटी सोने की हो फिर भी वह चाहेगा कि दूसरी एक घाटी का वह मालिक हो जाए। उसका मुँह तो बस मिट्टी ही से भरता है। ईश्वर का अनुग्रह उसपर होता है जो उसकी ओर पलटता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात् इनसान की चाहतें और कामनाएँ तो क़ब्र में ही जाकर समाप्त होती हैं। जीवन में उसकी इच्छाओं और कामनाओं का सिलसिला लम्बा ही होता जाता है, यहाँ तक कि यदि उसे सोने की घाटी भी प्राप्त हो जाए तो भी उसकी इच्छा होगी कि काश, ऐसी ही एक और घाटी उसके हिस्से में आ जाए! दुनिया में अनुचित इच्छाओं और लोभ-लालच से पीछा छुड़ाने में यदि कोई सफल हो सकता है तो वही व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में ईश्वर सम्मिलित हो गया हो। जब तक उसका विशेष अनुग्रह न हो, इनसान को इच्छाओं की ग़ुलामी से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन ईश्वर उन्हीं लोगों को संसार में सन्तोष-धन प्रदान करता और उन्हीं के दिल में अपनी कामना जगाता है जो उसकी ओर पलटते हैं, जो ईश्वर से अपने गुनाहों और कोताहियों के लिए क्षमा-याचना करते हैं और उसी के दामन में शान्ति, निश्चिन्तता और आराम की तलाश होती है।
प्रेम
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क़ियामत कब आएगी? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"अफ़सोस तुझपर, तूने उसके लिए क्या सामान कर रखा है?" उसने कहा कि मैंने तो उसके लिए कोई सामान नहीं किया है। सिवाए इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तू उसी के साथ होगा जिससे तू प्रेम करता है।" हमने कहा कि क्या हम भी इसी तरह होंगे? कहा, "हाँ" इस पर हम लोगों को उस दिन अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इतने में मुग़ीरा का एक ग़ुलाम जो मेरी उम्र का था, गुज़रा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “अगर यह जीवित रहा तो इसके बुढ़ापे से पहले ही क़ियामत आ जाएगी।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : जीवन में वास्तविक निर्णायक चीज़ प्रेम है। किसी आदमी के विषय में देखने की चीज़ यह नहीं होती कि उसके प्रत्यक्ष कर्म कैसे हैं। बल्कि देखने की चीज़ यह होती है कि कोई व्यक्ति स्वयं क्या है। इसका पता उसकी प्रेम-भावना ही से चलता है। अपने अन्तिम विश्लेषण में आदमी प्रेम ही है। देखना यह चाहिए कि प्रेम वह किससे और क्यों करता है। कर्म तो विभिन्न कारणों से परिमाण की दृष्टि से थोड़े भी हो सकते हैं किन्तु प्रेम और शुद्ध-हृदयता के अभाव या कमी की पूर्ति किसी और चीज़ से सम्भव नहीं। सौन्दर्य और सत्य से प्रेम न हो, यह मनुष्य का विनाश है।
सच्चा प्रेम कभी निष्प्रभावी नहीं रह सकता। प्रेम आदमी को उसके अभीष्ट और प्रेमपात्र का सामीप्य प्रदान करता है, बल्कि प्रेम स्वयं सामीप्य है। प्रेम जीवन का स्वभाव है। जिसका व्यक्तित्व किसी उच्च और पवित्र प्रेम से निर्मित न हुआ हो वह आत्मा और जीवन और प्रकाश से रहित है। सत्य यह है—
We are shaped and fashioned by what we love.
हम बने और सँवरे हैं उस प्रेम से जो हममें होता है।
हम अगर अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम कामयाब हैं। प्रेम और वफ़ादारी का प्रमाण कभी थोड़ा-सा धन ख़र्च करने से मिल जाता है और कभी अपार दौलत ख़र्च कर देने के बाद भी प्रेम का प्रमाण नहीं मिलता। ईश्वर दिलों को देखता है। वह जानता है कि किस धन-व्यय का प्रेरक अल्लाह और उसके रसूल का प्रेम है और किस धन-व्यय के पीछे कोई अन्य चीज़ कार्यरत है। वह इसकी ख़बर भी रखता है कि किसके अन्दर किस कोटि का प्रेम और निष्ठा पाई जाती है। इसी लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है कि कोई अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना (ईश्वरीय मार्ग में) व्यय कर दे तो किसी सहाबी के एक मुद (एक पैमाना जिसमें सेर भर जौ आता है) या आधे मुद के बराबर भी उसका सवाब न पहुँच सकेगा।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन कि “तू उसी के साथ होगा जिससे तू प्रेम करता है" के विषय में हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि "मैंने इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को किसी बात से भी इतना प्रसन्न होते नहीं देखा जितना वे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से हुए।"
प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न के उत्तर में कि क़ियामत कब आएगी, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुग़ीरा के ग़ुलाम की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह ग़ुलाम (जो कम उम्र है) अगर जीवित रहा तो इसके वृद्ध होने से पूर्व ही तुम्हारे संसार से विदा होने का समय आ जाएगा। और आदमी की मृत्यु ही उसके लिए अपनी क़ियामत है। इसलिए कि मृत्यु के बाद आदमी के साथ वे मामले शुरू हो जाते हैं जिनकी हैसियत कर्मों के प्रतिदान की है। क़ियामत इसी लिए तो आएगी कि इनसानों को उनके अपने कर्मों का प्रतिदान पूर्णतया मिल सके।
इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि किसी आदमी की मृत्यु और क़ियामत के घटित होने के दरमियान की अवधि उस आदमी को अत्यन्त कम महसूस होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि क़ियामत और मर कर जीवित होने की घड़ी के आने में बस इतना ही विलम्ब है जितना अपनी मौत के आने में। क़ुरआन में भी कहा गया है—
“जिस दिन वह उन्हें इकट्ठा करेगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे वे दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे।" (10:45)
(2) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह प्रेम करता है।" (हदीस : बुख़ारी)
(3) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि एक व्यक्ति किसी क़ौम से प्रेम करता है किन्तु वह उस क़ौम के लोगों से नहीं मिल सका। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह प्रेम करता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आदमी अपने जीवन में उन लोगों से न मिल सका जिनसे उसे प्रेम था। प्रेम के कारण अनिवार्यतः उसे अपने प्रेमपात्र का सामीप्य प्राप्त होगा। प्रेम जीवन के बुनियादी मूल्यों में से एक है। उसकी अनिवार्यताएँ अवश्य पूरी होकर रहेंगी।
जीवन की प्रत्येक चीज़ अपने अस्तित्व में शाश्वतता की सूचना रखती है। अगर ऐसा न हो तो वह निरर्थक होकर रह जाए। यहाँ की कोई चीज़ निरर्थक कदापि नहीं है। दृष्टिवान जानते हैं कि प्रत्येक क्षण पर शाश्वतता अपनी छाया डालती है। प्रेमभाव एक महत्वपूर्ण भाव है। उसे निरर्थक कैसे कह सकते हैं। प्रेम अनिवार्यतः स्थायी प्रभाव रखता है। वह कोई खो जानेवाली चीज़ नहीं हो सकती। वह अमर है। अमरता उसकी प्रकृति की महत्वपूर्ण माँग है। अमरता की तरह उसकी दूसरी अनिवार्यताएँ भी अवश्य पूरी होंगी।
(4) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर से प्रेम करो इसलिए कि वह नेमत के द्वारा तुम्हारा पालन-पोषण करता और आहार देता है, और मुझसे प्रेम करो ईश्वर से प्रेम के कारण, और मेरे घरवालों से प्रेम करो मेरे प्रेम के कारण।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात कुछ और नहीं तो इतना तो हर व्यक्ति समझ सकता है कि ईश्वर ही ने उसके पालन-पोषण और ख़ूराक आदि की व्यवस्था की है। ईश्वर के इस अनुग्रह के प्रति क्रियास्वरूप अनिवार्य है कि मानव अपने ईश्वर से प्रेम करे। ईश्वर के उपकारों और उसकी अनुकम्पाओं और अनुग्रहों का हक़ अगर मानव अदा कर सकता है तो इसी प्रकार कि वह उससे अपने सम्पूर्ण प्राण और सम्पूर्ण शक्ति के साथ प्रेम करे। फिर ईश्वर के इस प्रेम की अनिवार्यता यह भी है कि आदमी उसके रसूल से प्रेम करे। क्योंकि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर के प्रिय और उसके चुने हुए बन्दे हैं, और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रेम के लिए अनिवार्य यह है कि आदमी रसूल की सन्तान और आपके घरवालों से प्रेम करे।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रतापवान ईश्वर क़ियामत के दिन कहेगा कि वे लोग कहाँ हैं जो मेरे प्रताप के कारण परस्पर प्रेम करते थे। आज मैं उन्हें अपनी छाया में स्थान दूँगा। आज के दिन मेरी छाया के अतिरिक्त कोई अन्य छाया नहीं।” (हदीस : मुवत्ता)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि ईमानवालों को परस्पर प्रेम का सम्बन्ध रखना चाहिए। उन्हें ईमानवाले इसलिए कहा गया है कि वे ईश्वर की महानता से परिचित हैं। वे जानते हैं कि अगर वे ईश्वर के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं तो ईश्वरीय महानता और प्रताप उनसे प्रतिशोध लेकर रहेगा। यह ईश्वर का हक़ है कि बन्दा उससे प्रेम करे और उन लोगों से भी प्रेम करे जिनका ईश्वर से प्रेम का सम्बन्ध है। ईश्वर की महानता का एहसास मोमिन को प्रत्येक प्रकार के अन्याय से रोकता है। मोमिन परस्पर प्रेम के रिश्ते में जुड़े होते हैं। ईश्वर की महानता और श्रेष्ठता की सामूहिक चेतना और इसका उभयनिष्ठ एहसास दूसरे समस्त एहसासों पर छा जाता है। इसके कारण मोमिनों में एक ऐसी एकात्मता पैदा हो जाती है जिसकी मिसाल पेश करने में दुनिया असमर्थ है। उनकी एकात्मता और उनकी एकता को कोई भी चीज़ आघात नहीं पहुँचा सकती। वास्तव में वे अपना सांसारिक जीवन भी ईश्वर ही की छाया में व्यतीत करते हैं जबकि ईश-ज्ञान से अपरिचित लोगों के जीवन मात्र भौतिक लाभ की इच्छा और क्षणिक सुख-सुविधाओं के सहारे व्यतीत होते हैं। यह तथ्य आज नहीं तो कल उजागर होकर रहेगा। अतएव कहा गया कि ईश्वर क़ियामत के दिन उन लोगों को जो परस्पर ईश्वर की महानता और प्रताप के कारण आपस में प्रेम का सम्बन्ध रखते थे, अपनी छाया में स्थान देगा। उस दिन उसकी छाया के अतिरिक्त और कोई छाया न होगी। झूठी निश्चिन्तताएँ और पनाहगाहें उस दिन शेष न रह सकेंगी। झूठे सहारे टूट चुके होंगे।
(6) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को कभी इतना प्रसन्न होते नहीं देखा जितना वे इसपर प्रसन्न हुए। एक व्यक्ति ने कहा कि “ऐ अल्लाह के रसूल! एक व्यक्ति एक आदमी से उसके नेक कर्म के कारण प्रेम करता है यद्यपि वह स्वयं उस जैसा कर्म नहीं करता।" नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह प्रेम करता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : जीवन के आधारभूत मूल्यों में से हरेक मूल्य इतना संग्राहक है कि उसे ही धर्म का शीर्षक निर्धारित किया जा सकता है, और उसके प्रकाश में धर्म की व्याख्या की जा सकती है। इसके अतिरिक्त चिन्तन के उच्चतम स्तर पर समस्त जीवन-मूल्य परस्पर मिलकर इस प्रकार एकरस हो जाते हैं कि उनमें कोई अन्तर शेष नहीं रहता।
प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य और एक महत्वपूर्ण भाव है। धर्म ने इसे मौलिक महत्व दिया है। इस्लाम के बारे में जो लोग ग़लतफ़हमियों के शिकार हैं वे कहते हैं कि इस्लाम एक कट्टरतावादी धर्म है। काश वे समझ सकते कि कितनी ग़लत बात उनके मुख से निकल रही है। इस्लाम तो वास्तव में प्रेम का धर्म है। इस्लाम और उसकी धारणाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन के तथ्यों (Facts) को समझे। इस्लाम जीवन की वास्तविकताओं से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए इस्लाम को मार्गदर्शन से अभिव्यंजित किया गया है। ऐकेश्वरवाद और परलोक की धारणा को लीजिए, दोनों ही का जीवन के उन सत्यों से गहरा सम्बन्ध है जिनकी उपेक्षा अन्धापन और पथभ्रष्टता है। इस्लाम-विरोधी धारणाओं को इसी लिए पथभ्रष्टता कहा गया है कि उनमें जीवन के तथ्यों की प्रत्यक्षतः उपेक्षा की गई है। आख़िरत में दूसरी कोई चीज़ नहीं बल्कि जीवन ही के तथ्य प्रकाशित होंगे। जिस प्रकार आप आम का वृक्ष लगाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपका लगाया हुआ यह वृक्ष फल देने लगता है। फल देने से पूर्व भी उससे आपको हरियाली और छाया प्राप्त होती है, लेकिन समय आने पर यह आपको इसके अतिरिक्त मीठे फल भी देने लगता है और उस वृक्ष के अन्दर जो सम्भावनाएँ पाई जाती रही हैं वे प्रत्यक्ष हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार इस वर्तमान जीवन की जो सम्भावनाएँ हैं उनसे हम इस संसार में भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक चरण ऐसा आएगा कि जीवन की सम्भावनाएँ पूर्णरूप से प्रकाश में आ जाएँगी और आदमी शाश्वत ईश-प्रसादों से लाभान्वित होगा। सारांश यह कि आख़िरत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस जगत् और वर्तमान जीवन के अनुकूल न हो, बल्कि सत्य यह है कि आख़िरत वर्तमान जीवन की सम्भावनाओं ही की पूर्ण अभिव्यक्ति है।
वर्तमान जीवन में प्रेम से सभी परिचित हैं। प्रेम का प्रभाव लोक-परलोक दोनों को व्याप्त है। मोमिन के जीवन में प्रेम को बड़ा महत्व प्राप्त है। ईश्वर स्वयं अपने नेक बन्दों से प्रेम करता है। प्रेम की भावना अत्यन्त सुदृढ़ और पवित्र होती है। प्रेम में हृदय को समस्त दुर्भावनाओं और प्रदूषणों से मुक्त करने की शक्ति है। ईश्वर प्रभु ही नहीं, प्रियतम भी है। उसकी अगर किसी को पहचान हो जाए तो वह अनिवार्यतः उससे प्रेम करेगा और उसकी उपासना और आज्ञाकारिता में सक्रिय होगा। ईश्वर की राह में संघर्ष करने में भी वह पीछे नहीं रह सकता। ईश्वर से प्रेम करने वालों के पारस्परिक सम्बन्धों में भी प्रेम ही क्रियाशील होगा। वे परस्पर एक-दूसरे के दीन और ईमान और जान व माल के भी रक्षक सिद्ध होंगे।
प्रेम और मैत्रीभाव इस सांसारिक जीवन की भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिसका कोई दोस्त न हो उसका जीवन नीरस और रंगहीन होगा। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सलमा-बिन-अकवअ को चमड़े की ढाल उपहार स्वरूप दी थी। उन्होंने उसे किसी व्यक्ति को दे दिया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे पूछा कि सलमा तेरी ढाल कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त को दे दी। इसपर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ऐ ख़ुदा, तू मुझे ऐसा दोस्त दे जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा हो।” (हदीस : मुस्लिम)
प्रेम स्वयं भी नेमत है। यह स्वयमेव जीवन को अपेक्षित है। प्रेम वह प्रकाश है जिससे ईश्वर की पहचान होती है। प्रेम नूर है, प्रेम ज्ञान है।
नेक व्यक्ति का हक़ है कि हम उससे प्रेम का सम्बन्ध रखें। इसके द्वारा हमें उसका साहचर्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए कि प्रेमभावना वह भावना है जिसका महत्व और मूल्य बहरहाल शेष रहता है। अगर ईश्वर के वफ़ादार बन्दों से हम सच्चा प्रेम करते हैं तो कामयाबी का सिरा हमारे हाथ में है। सच्चे प्रेम का प्रमाण कभी सिर्फ़ दिल ही जुटा देता है और कभी, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, अपार धन व्यय कर देने के पश्चात भी प्रेम का प्रमाण नहीं मिलता। ईश्वर वास्तव में हमारे दिलों को देखता है।
(7) हज़रत ज़ैद ख़ैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! उस व्यक्ति में ईश्वर की क्या निशानी है जिसको वह चाहे, और जिसको वह न चाहे उस में उसकी क्या पहचान है? कहा कि “ऐ ज़ैद! तुमने किस हाल में सुबह की?” मैंने कहा कि इस हाल में कि नेकी और नेकी करनेवालों से मुझे प्रेम है, और अगर मैं नेकी की सामर्थ्य रखता हूँ तो उसे जल्द करता हूँ और अगर नेकी छूट जाए तो दुखी हो जाता हूँ और रो पड़ता हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि ईश्वर की यही निशानी उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसको वह चाहता है। और अगर वह तेरे लिए किसी और चीज़ का इरादा करता तो ऐसा करता कि तुझे उस के लिए तत्पर कर देता।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि ईश्वर के यहाँ स्वीकार्यता का संकेत यह है कि आदमी को भलाई और भलाई करनेवालों से प्रेम हो। सामर्थ्य हो तो नेकी से न रुके, बल्कि नेकी और भलाई के कामों की ओर लपक पड़े और अगर कहीं नेकी न कर सके तो इससे उसे दुख हो। नेकी से किसी की रुचि इस बात का स्पष्ट लक्षण है कि ईश्वर उसे चाहता है और अगर आदमी भलाई और शुभ के अतिरिक्त किसी और चीज़ के लिए तत्परता दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर का प्रिय बन्दा नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने उसे दूसरे कामों के लिए छोड़ दिया। क़ुरआन में है—
"रहा वह व्यक्ति जिसने कृपणता अपनाई, और उपेक्षा की, और अच्छी चीज़ को झुठला दिया, उसे हम उस चीज़ का पात्र बना देंगे जो कष्ट-साध्य है।" (92: 8-10)
(8) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— "तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति में पाई जाएँ उसे ईमान का स्वाद और आनन्द प्राप्त होगा। यह कि ईश्वर और उसका रसूल उसे शेष सबसे अधिक प्रिय हों, और यह कि किसी व्यक्ति से उसे प्रेम हो तो यह प्रेम मात्र ईश्वर के लिए हो, और यह कि वह कुफ़्र की ओर पलटने को, जबकि ईश्वर ने उसे उससे निकाल लिया हो, ऐसा बुरा समझे जैसा कि इसको बुरा समझता है कि उसे आग में फेंक दिया जाए।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि ईमान के स्वादप्रद और भावपूर्ण होने का वास्तविक रहस्य प्रेमभाव है। जब आदमी के विचारों और उसके जीवन के तमाम मामलों में प्रेम एक क्रियाशील शक्ति की हैसियत प्राप्त कर लेता है तो उस समय उसे उस आस्वादन और आनन्द से परिचित होने में विलम्ब नहीं होता जिसकी सूचना इस हदीस में दी गई है।
जिस तथ्य का इस हदीस में उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख इस प्रसिद्ध हदीस में भी मिलता है—
"ईमान का मज़ा चख लिया उस व्यक्ति ने जो ईश्वर के रब होने, इस्लाम के धर्म होने और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रसूल होने पर राज़ी हो गया।" (हदीस : मुस्लिम)
यह एक सच्चाई है कि मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है और वही उसका पालनकर्ता है। उसके जीवन की पूर्णत्व प्राप्ति की कल्पना भी हम प्रभु के बिना नहीं कर सकते। मानव अपनी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार की आवश्यकता के लिए अपने प्रभु पर आश्रित है। ईश्वर की पालनक्रिया हमारे लिए उसकी सबसे बड़ी कृपा है। ज्ञानवान है वह व्यक्ति जो ईश्वर की इस पालनक्रिया पर मुग्ध और प्रसन्न है।
आदमी का धर्म इस्लाम हो, यह ईश्वर को प्रभु मानने की स्वाभाविक अनिवार्यता है। इसलिए कि इस्लाम का अर्थ ही यह होता है कि आदमी ईश्वर की प्रभुता अर्थात उसकी कारफ़रमाई और कारसाज़ी से अपने को अलग न रखकर स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। यह समर्पण जीवन को एक विशिष्ट शैली (Pattern) में ढाल देता है। इसे ही इस्लाम के नाम से परिभाषित किया गया है। इसलिए इस्लाम को एक धर्म और जीवन प्रणाली के रूप में अपनाना ही मानव का मूल स्वभाव और प्रकृति है। अपनी प्रकृति की माँग को पूरा करके ही आदमी उस आनन्द और आस्वाद को प्राप्त कर सकता है जिसकी तलब प्रत्येक हृदय में रखी गई है। वास्तव में उसी व्यक्ति को ईमान से लाभान्वित कहेंगे जिसका जीवन प्रकृति की इस माँग की पूर्ति का पर्याय हो।
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर के प्रतिनिधि और उसके रसूल हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आमन्त्रण इसके सिवा और कुछ नहीं कि मानव अपनी प्रकृति से परिचित हो और उसकी मौलिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने की ओर से ग़ाफ़िल न हो। ऐसे रसूल के मार्गदर्शन को स्वीकार करने से ज़ाहिर है मानव के लिए अपार हर्ष और आनन्द के दरवाज़े खुल जाते हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ईशदूतत्व को स्वीकार किए बिना सम्भव नहीं कि मानव को वे प्रसन्नताएँ प्राप्त हो सकें जो सत्य से परिचित प्रत्येक व्यक्ति की नियति हैं।
इस प्रकार यह भली-भाँति स्पष्ट होता है कि ईमान उन तीन सत्यों को माने बिना, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, आत्मारहित और निष्फल रहता है और मानव जीवन असफल और त्रासदी बनकर रह जाता है।
ग़ैरत (स्वाभिमान)
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईश्वर स्वाभिमानी है और मोमिन भी स्वाभिमानी होता है। और ईश्वर के स्वाभिमान की अपेक्षा यह है कि मोमिन उस काम को न करे जिसको ईश्वर ने हराम क़रार दिया है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ईश्वर ने इनसान को प्रतिष्ठा और महानता प्रदान की है। इनसान का कर्तव्य है कि वह इस प्रतिष्ठा के मूल्य और महत्व को पहचाने और उसे किसी प्रकार भी आहत न होने दे। मनुष्य में ग़ैरत या स्वाभिमान इसी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए रखा गया है। जिन कामों के करने से आदमी की प्रतिष्ठा आहत होती है ईश्वर ने उनको उसके लिए हराम क़रार दिया है। ईश्वर केवल यही नहीं चाहता कि मानव के अस्तित्व की सुरक्षा हो, बल्कि वह यह भी चाहता है उसकी प्रतिष्ठा पर भी कोई आँच न आए। यह ईश्वर का आत्यान्तिक अनुग्रह और उसकी अनुकम्पा है। उदाहरणार्थ ईश्वर ने शिर्क और व्यभिचार को अवैध ठहराया है। हम देखते हैं कि यह दोनों ही चीज़ें मानव के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा के प्रतिकूल हैं। जिस प्रकार व्यभिचार से मानव की गरिमा शेष नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार शिर्क (बहुदेववाद) भी मानव के लिए एक लज्जाजनक कार्य है जिसके कारण मानव की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा और पवित्रता शेष नहीं रहती। बहुदेववाद भी मानव से उसकी इज़्ज़त छीन लेता है। क़ुरआन ने सूरा नूर में बहुदेववाद और व्यभिचार को एक साथ वर्णन करके यह संकेत किया है कि बहुदेववाद और व्यभिचार में कोई तात्विक अन्तर नहीं है। मानव के लिए दोनों ही समान रूप से बुरे हैं।
इस हदीस से यह बात भी मालूम होती है कि ईश्वर का अपने बन्दों से अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है। यही कारण है कि वह इसे अपनी ग़ैरत के ख़िलाफ़ समझता है कि बन्दे उन कार्यों में लिप्त हों जो उसकी अपनी महानता और उच्चता को शोभनीय नहीं। उसके लिए अपने बन्दे की रुसवाई और पतितता असहनीय है।
(2) हज़रत मुग़ीरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि साद-बिन-उबादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि अगर मैं किसी परपुरुष को अपनी पत्नी के साथ देखूँ तो अवश्य ही मैं उसपर तलवार से वार करूँ। तलवार के चौड़े पहलू से नहीं (बल्कि धार की ओर से)। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक यह बात पहुँची तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या तुम्हें साद की ग़ैरत पर आश्चर्य है, ईश्वर की सौगन्ध, मैं उससे ज़्यादा ग़ैरतमन्द हूँ और ईश्वर मुझसे बढ़कर ग़ैरतमन्द है। और यह ईश्वर की ग़ैरत ही है जिसके कारण ईश्वर ने खुले और छिपे समस्त निर्लज्जता के कार्यों को वर्जित किया है। और ईश्वर से बढ़कर कोई उज़्र (आपत्ति) के दूर करने को पसन्द करनेवाला नहीं। इसी लिए उसने सचेत करनेवाले और शुभ-सूचना देनेवाले पैग़म्बर भेजे। और ईश्वर से बढ़कर किसी को प्रशंसा भी पसन्द नहीं हो सकती। इसी लिए ईश्वर ने स्वर्ग का वादा किया है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मूल में यहाँ ‘उज़्र' शब्द आया है। नववी की दृष्टि में ‘उज़्र' यहाँ ‘एज़ार' अर्थात उज़्र दूर करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ईश्वर ने नबियों और रसूलों को सचेतकर्ता और शुभ-सूचक बनाकर इसी लिए भेजा ताकि कोई व्यक्ति यह उज़्र न पेश कर सके कि उसे तो वास्तविकता की ख़बर ही न थी। क़ुरआन में भी आया है— “रसूल ख़ुशख़बरी देनेवाले और डरानेवाले बनाकर भेजे गए ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुक़ाबले में कोई तर्क न रहे, अल्लाह तो है ही अत्यन्त प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी।" (4 : 165)
ईश्वर सारे ही गुणों और सौन्दर्य का मालिक है। मानव के चिन्तन और विचार की उन्नति इसपर निर्भर करती है कि उसे ईश्वर का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी कि आदमी दुनिया में सारी बातों के सम्बन्ध में ज्ञान अर्जित करे किन्तु अपने प्रभु के गुण, उसके सौन्दर्य और कौशल्य से अनभिज्ञ रहे। बन्दा ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा उसी समय कर सकता है जबकि उसे अपने प्रभु की सही पहचान हो। इनसान क्या धारणाएँ और विश्वास रखे और वह अपने जीवन में कौन-सी नीति अपनाए, इस सम्बन्ध में ईश्वर ने जो मार्गदर्शन किया है वह इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि ईश्वर प्रशंसनीय और स्तुति का पात्र है। अब अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की अवज्ञा करता है तो इसका मतलब इसके सिवा और क्या होगा कि वह जीवन के लिए ऐसे आदेशों का इच्छुक है जो वही दे सकता है जो हमारी प्रशंसा का पात्र न हो। उदाहरणार्थ— शिर्क, अज्ञान, अधमता और नीचता की शिक्षा तो ईश्वर देने से रहा। इस प्रकार की शिक्षा तो शैतान ही की हो सकती है जो, तिरस्कृत और घृणित है।
लज्जा और शर्म
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक व्यक्ति के पास से गुज़रे। वह लज्जा के सम्बन्ध में (किसी पर) क्रोधित हो रहा था। कह रहा था कि तुम इतनी लज्जा करते हो कि उससे तुम्हें हानि पहुँचेगी। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "उसे छोड़ दो, इसलिए कि लज्जा ईमान का एक अंश है।" (हदीसः बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस व्यक्ति से जो कुछ कहा उसका अर्थ यह है कि तुम लज्जा करने से न रोको। लज्जा तो एक मूल्यवान नैतिक गुण है और ईमान का लक्षण भी है। ईश्वर के असीम उपकारों को देखकर एक सजग व्यक्ति सोचता है कि उसे अपने ईश्वर का कृतज्ञ बन्दा बनकर रहना चाहिए। यही ईश्वर के उपकारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन इस बात को इन्सान अकसर भूल जाता है। इन्सान को अकृतज्ञता से रोकनेवाली कई चीज़ें हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, ईश्वर के प्रकोप का डर, उसके उपकारों से वंचित हो जाने का भय, आदि। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए अवज्ञा और अकृतज्ञता की नीति अपनाने में लज्जा रुकावट बनती है वह सोचता है कि ईश्वर के उपकारों के बदले में वह अकृतज्ञता की नीति अपनाए तो कैसे अपनाए। ऐसे व्यक्ति की पवित्र और स्वच्छ आत्मा की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लज्जा ईश्वर से उसके ऐसे सम्बन्ध का प्रतीक है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण और आनन्ददायक है।
इस हदीस में हया को ईमान का अंश कहा गया है। इससे मालूम हुआ कि ईमान समस्त गुणों का संग्राहक है। ईमान वास्तव में एकेश्वरवाद को स्वीकार करना है। एकेश्वरवाद का जीवन के तमाम पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। जीवन की किसी चीज़ को भी एकेश्वरवाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपने सम्पूर्ण जीवन से और अपने सम्पूर्ण जीवन में जिसने ईश्वर को पहचाना उसी ने ईश्वर को ज़्यादा पहचाना। हमारे सम्पूर्ण जीवन में ईश्वर हमारे साथ है। जीवन के प्रत्येक मामले में वह हमारा मार्गदर्शन करता है। अतः हमें अपने सम्पूर्ण जीवन के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए कि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं।
In all thy ways acknowledge Him.
हमारे जीवन की प्रत्येक शैली और प्रत्येक तरीक़े से हमारी ईमानी कैफ़ियत का इज़हार हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव आत्मा अपने को जीवन की विभिन्न शैलियों और रूपों में व्यक्त करती है, आवश्यक है कि हम ईश्वर को अपने पूरे जीवन के द्वारा स्वीकार करें। हमारे पास ईश्वर को जानने का साधन जीवन ही है, और यह निकटतम साधन है। सजदे की तरह हमारा जीवन भी ईश्वर के सामीप्य का साधन बल्कि स्वयं सामीप्य बन सकता है, और यह सामीप्य हमारे अस्तित्व और जीवन का अवयव हो सकता है। यह बात कितनी आनन्ददायक है।
ईमान का सम्बन्ध हमारे सम्पूर्ण जीवन और उसकी गतिविधियों से है। यह ईमान मोमिन के जीवन में समस्त गुणों का संग्राहक है। स्वर्ग सद्गुणों और सौन्दर्य का ख़ज़ाना है। दुनिया में जहाँ कहीं और जिस रूप में कोई गुण नज़र आता है उसका सम्बन्ध स्वर्ग ही से है। इसी लिए कहा गया है कि "ईमान का स्थान स्वर्ग है।" (हदीस)
ख़ूबी तो यह है कि बुराई के रास्ते में आदमी स्वयं रोक बन जाए। इसके बिना बुराई से घृणा और वास्तविक दूरी पैदा नहीं हो सकती। इसी तरह यह भी अभीष्ट है कि नेकी का प्रेरक व्यक्ति स्वयं हो। इसके बिना मानव सही अर्थों में नेक कहे जाने का पात्र नहीं बन सकता।
लज्जा की एक अपेक्षा यह है कि हम निगाह को बचाएँ। जो व्यक्ति नज़र की रक्षा नहीं करता उसका दिल आवारा हो जाता है। निगाह के साथ दिल भी लगा होता है। नज़रों को झुकाए रखने की शरीअत में इसी लिए बड़ी ताकीद आई है। लज्जा एकान्त में भी अपेक्षित है। इसलिए कि कोई और नहीं तो ईश्वर इस हालत में भी आदमी के साथ होता है। संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं अपने से भी लज्जा करते हैं।
(2) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"पूर्वकाल की नुबूवत की वाणी में से लोगों ने जो कुछ पाया है, उसमें से एक यह है कि “जब तुम्हें लज्जा नहीं तो अब जो चाहो करो।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मानव समाज पर नबियों की शिक्षाओं ने गहरे प्रभाव डाले हैं। बिगड़े से बिगड़े समाज में भी कितनी ही ऐसी नेक बातें मुहावरों और लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हैं जो वास्तव में पिछले नबियों की शिक्षाओं का अवशेष हैं किन्तु हमें इसकी ख़बर नहीं होती। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं कि यह लोकोक्ति कि 'जब तुम्हें लज्जा नहीं तो अब जो चाहो करो', पूर्वकाल की नुबूवत की वाणी में से है। इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि पिछले नबियों की शिक्षाओं में भी गहरी तत्वदर्शिता और सदुपदेश पाया जाता था। इस कथन की तरह और भी कितनी ही उक्तियाँ लोगों की ज़बानों पर चढ़ी हुई हैं जिनमें पूर्वकालीन नबियों की शिक्षाओं की छाया देखी जा सकती है।
इस हदीस से मालूम हुआ कि हया और शर्म की शिक्षा केवल नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही नहीं दे रहे थे बल्कि उसको पिछले नबियों के युगों में भी मौलिक महत्व प्राप्त रहा है। लज्जा और शर्म वास्तव में एक सूक्ष्म आन्तरिक प्रेरणा है जो आदमी को अनुचित और अशोभनीय कामों से रोकती है। इस आन्तरिक कैफ़ियत के कारण आदमी के व्यक्तित्व में बड़ा आकर्षण पैदा हो जाता है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में हदीस में आया है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कुँआरी लड़कियों से भी ज़्यादा लज्जावान थे। हदीस में ईश्वर के बारे में भी आया है कि ईश्वर को अपने बन्दे से इस बात पर शर्म आती है कि जब उसका बन्दा अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाए तो वह उन्हें ख़ाली वापस करदे। (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
इस हदीस में यह बात कही गई है कि जिस व्यक्ति के अन्दर लज्जा नहीं है वह जो बुराई करे कम है। इसलिए कि वास्तव में जो चीज़ उसे बुराई से रोकने वाली थी जब वही जाती रही तो फिर कौन-सी चीज़ उसे ईश्वर की अवज्ञा और बुरे कामों से रोक सकती है। हया एक व्यक्तिगत गुण है। जिसमें यह गुण मौजूद है वह स्वयं अपने आन्तरिक तक़ाज़े से बाध्य होकर निर्लज्जता से बचेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे नीबू का पेड़ ज़मीन से उन ही तत्वों को लेगा जो उसके स्वभाव और उसके गुणों के अनुकूल होंगे। वह दूसरे तत्वों को छोड़ देगा। गन्ना और शकरकंद भूमि से उन तत्वों को ऐसे रूप में लेंगे कि उनमें मिठास पैदा हो सके। इसके विपरीत नीम का वृक्ष मिट्टी से ऐसे तत्वों को लेगा कि उसमें तीक्ष्णता और कड़ुवाहट आ सके।
(3) हज़रत इमरान-बिन-हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा भलाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं लाती।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : लज्जा अपने परिणाम की दृष्टि से किसी हानि और अशुभ का कारण नहीं बनती। एक और हदीस में है कि लज्जा सर्वथा भलाई है। बेशर्मी अपने परिणाम की दृष्टि से सरासर घाटे का सौदा है। हया को छोड़कर आदमी सबसे पहले स्वयं अपने व्यक्तित्व को नुक़सान पहुँचाता है। इससे उसकी गरिमा इतनी आहत हो जाती है कि उसकी क्षतिपूर्ति की सम्भावना बहुत कम रह जाती है।
(4) हज़रत जैद-बिन-तलहा-बिन-रुकाना (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रत्येक धर्म का एक मिज़ाज (स्वभाव) होता है, इस्लाम का मिज़ाज लज्जा है।" (इब्ने-माजा, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : मुवत्ता में इमाम मालिक ने इस हदीस को ज़ैद-बिन-तलहा से रिवायत किया है। ज़ैद-बिन-तलहा ताबई हैं। उन तक यह हदीस किसी सहाबी के द्वारा पहुँची। इसका उल्लेख इमाम मालिक ने नहीं किया। अलबत्ता इब्ने-माजा और बैहक़ी ने अपनी सनद के साथ इसे दो सहाबियों हज़रत अनस और हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत किया है।
जीवन की कोई भी धारणा या पद्धति हो, अनिवार्यतः उसका अपना एक विशिष्ट स्वभाव होगा और वह एक विशिष्ट अभिरुचि को व्यक्त करेगी। इसी मिज़ाज, मूल आत्मा और अभिरुचि की दृष्टि से हम उसके मूल्य का अनुमान कर सकते हैं। इस्लाम मनोविज्ञान के विश्वसनीय और नाज़ुक और सूक्ष्मतर तथ्यों पर आधारित धर्म है। लज्जा को इस्लाम का मिज़ाज कहा जा रहा है। यह इसका स्पष्ट प्रमाण है। मालूम हुआ कि पूर्ण मुस्लिम वही है जिसके अन्दर लज्जा हो। जो ईश्वर से भी लज्जा करता हो जिसने उसे अस्तित्व प्रदान किया और इन्सानों से भी लज्जा करता हो जिनके मध्य वह जीवनयापन करता है। उसके मिज़ाज को उन बातों से घृणा हो जो अश्लील और अशिष्ट हों। उसे ईश्वर के अधिकारों का भी ध्यान हो और लोगों के अधिकारों का भी वह ध्यान रखता हो।
(5) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“हया और ईमान एक साथ रहते हैं, जब इनमें से कोई एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है।" (हदीस अल-बैहक़ी फ़ी शोअ्बिल ईमान)
व्याख्या : जहाँ चराग़ होता है, उसके साथ रौशनी भी होती है। दोनों में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। यह सम्भव नहीं कि चराग़ तो हो मगर रौशनी न हो। इसी प्रकार हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि रौशनी हो मगर चराग़ के बिना। ठीक यही हाल ईमान और लज्जा का है। ईमान है तो उसका गुण लज्जा भी उसके साथ होगा। और अगर आदमी के अन्दर हया (लज्जा) नहीं है तो समझ लीजिए कि उसका दिल ईमान के उच्चतर गुणों से रिक्त है।
एक रिवायत में "जब उनमें से कोई एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है" के स्थान पर ये शब्द आए हैं कि “जब उनमें से कोई एक छिन जाता है तो दूसरा भी उसके पीछे चला जाता है।"
(6) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अश्लीलता और निर्लज्जता की बात जिस चीज़ में भी पैदा हो जाए वह उसे अनिवार्यतः ऐबदार और कुरूप बना देती है और लज्जा जिस चीज़ में शामिल हो उसे सुन्दर बना देती है।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह हदीस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सौन्दर्यपरक मूल्यों का ध्यान रखना सामान्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी आवश्यक है। जिस चीज़ में सौन्दर्य के स्थान पर कुरूपता हो वह चीज़ मूल्यहीन समझी जाएगी। लज्जा का ध्यान रखना वास्तव में सौन्दर्यबोध को महत्व देना है।
पाकदामनी और संयम
(1) हज़रत सहल-बिन-साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति अपने दोनों जबड़ों और अपनी दोनों टांगों के मध्य की चीज़ों की ज़मानत दे तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के मध्य की चीज़ों से अभिप्रेत जिह्वा (ज़बान) और गुप्तांग हैं। हम कितने पाकदामन हैं और हममें कितना संयम पाया जाता है इसका अन्दाज़ा इन दोनों चीज़ों से भली-भाँति किया जा सकता है।
आदमी वही बात कहे जो सही और दुरुस्त हो और जिसके कहने की आवश्यकता भी हो तो यह उसके विश्वासपात्र होने का स्पष्ट प्रमाण है। जिह्वा के प्रयोग में सावधानी बरतना और उत्तरदायित्व का एहसास आदमी को चरित्र की दृष्टि से इतनी उच्चता और गरिमा प्रदान कर सकता है जिसकी सामान्य परिस्थिति में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क़ुरआन में भी है—
“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का डर रखो और बात कहो ठीक सधी हुई। वह तुम्हारे कर्मों को सँवार देगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा।" (33:70-71)
दूसरी चीज़ जिसकी रक्षा की ताकीद इस हदीस में की गई है वह गुप्तांग है। यौन-प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली प्रवृत्ति है कि अगर इसके मामले में मानव असन्तुलन और स्वच्छन्दता का शिकार हो जाए तो इसके जो ख़तरनाक परिणाम अश्लीलता, निर्लज्जता और नग्नता के रूप में सामने आते हैं उनसे हर व्यक्ति परिचित है। स्वच्छन्द यौनाचार सम्पूर्ण समाज के विनाश का कारण बन सकता है। यौन-प्रवृत्ति, जिसकी हैसियत एक बड़ी नेमत की है और जिसपर मानवजाति का अस्तित्व निर्भर करता है, स्वछन्दता और आवारगी की भेंट चढ़कर व्यक्ति, परिवार और सम्पूर्ण समाज के लिए एक संकट और यन्त्रणा बन सकती है। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता ने इसके जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं।
(2) हज़रत-इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति भूखा या मुहताज हो और अपनी हालत को लोगों से छिपाए तो प्रतापवान ईश्वर पर यह हक़ है कि वह उसके लिए वैध तरीक़े से साल भर की आजीविका की व्यवस्था कर दे।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : अर्थात जो व्यक्ति भूख और तंगी की तकलीफ़ों को सहन कर लेता है लेकिन अपने को रुसवा होने नहीं देता तो ईश्वर अनिवार्यतः उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा में उसकी सहायता करता है और उसके लिए उसकी आजीविका का कोई न कोई प्रबन्ध कर देता है, लेकिन ईश्वर की सहायता उसे उसी समय तक मिलती रहती है जब तक उसे अपनी प्रतिष्ठा के मूल्य और लज्जा का ध्यान रहता है।
यह हदीस बताती है कि आदमी के पास सर्वाधिक मूल्यवान चीज़ उसका अपना व्यक्तित्व है। उसके आहत होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अपनी गरिमा को आहत करते हुए वह अगर लोगों से कोई सहायता प्राप्त करता है तो यह बड़े ही घाटे का सौदा है। इसलिए कि एक मूल्यवान चीज़ खोकर उसने जो वस्तु प्राप्त की वह उसके मुक़ाबले में कुछ भी नहीं है। आदर्श समाज वही हो सकता है जिसमें न केवल यह कि लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो बल्कि वह लोगों की इज़्ज़त और आबरू और उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षा की ज़मानत भी दे।
(3) हज़रत इमरान-बिन-हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईश्वर अपने उस मोमिन बन्दे से प्रेम करता है जो मुहताज, पाकदामन और बाल-बच्चोंवाला हो।” (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : अर्थात इसके बावजूद कि वह मुहताज और ज़रूरतमन्द है, बाल-बच्चे भी उसके साथ हैं जिनका भरण-पोषण भी उसे करना होता है, उसे अपनी इज़्ज़त-आबरू और प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान है। तंगी और परेशानी में गुज़ारा करता है लेकिन न वह हराम कमाई की ओर लपकता है और न लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता है। ईश्वर का अपने ऐसे बन्दों से विशिष्ट सम्बन्ध होता है। वे उसे प्रिय होते हैं।
(4) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति ईश्वर से थोड़ी-सी आजीविका पर राज़ी हो तो ईश्वर उससे थोड़े से कर्म पर राज़ी हो जाता है।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : ईश्वर की दी हुई थोड़ी-सी आजीविका पर राज़ी रहना वास्तव में आदमी के स्वभाव की निर्मलता और स्वस्थता का एक बड़ा प्रमाण है। निर्मल स्वभाव इतना बड़ा गुण है कि अगर आदमी के पास प्रत्यक्षतः नेक कर्मों की बहुलता न भी हो तो इसके द्वारा यह कमी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर यह गुण न पाया जाता हो तो कोई दूसरी चीज़ इसका विकल्प नहीं हो सकती। वास्तविक महत्व और मूल्य निर्मल स्वभाव और स्वस्थ हृदय का है। क़ुरआन में है—
“जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, सिवाय इसके कि कोई भला-चंगा हृदय लेकर ईश्वर के समक्ष उपस्थित हुआ।” (26:89)
यह हदीस बहुत ख़ूबसूरत है। यहाँ अवसर नहीं कि इसके साहित्यिक गुणों की ओर कुछ संकेत किए जाएँ। साहित्य प्रेमी इसके साहित्यिक सौंदर्य को भली-भाँति महसूस कर सकते हैं।
(5) हज़रत शद्दाद-बिन-औस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने मन को नियन्त्रित रखे और कर्म मृत्यु पश्चात के लिए करे। और लाचार व्यक्ति वह है कि जो अपनी इच्छाओं का दास हो और ईश्वर से कामनाएँ करता हो।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : आदमी वह नीति अपनाए जो उसके लिए अधिक से अधिक फ़ायदेमन्द हो। यही बुद्धिमत्ता है। इस पहलू से जब हम देखते हैं तो यह हदीस हमें बताती है कि आदमी की समस्त सफलताओं का रहस्य इसमें है कि वह अपने मन को गुमराह न होने दे। उसपर नियंत्रण रखे और अधैर्य का शिकार हो जाने से उसे बचाए। दृष्टि में वह हो जो विश्वसनीय हो अर्थात वह जीवन जो मृत्योपरान्त मिलनेवाला है, जिसे भावमय और आनन्ददायक बनाने के लिए हमें वर्तमान जीवन में चारित्रिक उच्चता का प्रमाण देना है। अगर हम इस दायित्व को महसूस नहीं करते तो हमारा मृत्योपरांत जीवन अत्यन्त त्रासदी जनक और अपमानजनक होगा जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए कठिन है।
जब वास्तविकता यह है तो वह व्यक्ति कितना नादान और नाकारा है जो ईश्वर से बड़ी आशाएँ रखे और इस सम्बन्ध में अपने दायित्वों का उसे कोई एहसास न हो और उसने अपनी सारी उर्जा और अभिरुचि वासनाओं की पूर्ति में लगा रखी हो।
अनासक्ति (Unattachment)
(1) हज़रत सुहैल-बिन-साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा—
“ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसा कोई कर्म बताएँ कि जब मैं उसे करूँ तो ईश्वर भी मुझसे प्रेम करे और लोग भी मुझसे प्रेम करने लगें।" रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "दुनिया की ओर से अनासक्त (बेनियाज़) हो जाओ तो ईश्वर तुमसे प्रेम करने लगेगा, और जो कुछ लोगों के पास है उससे अनासक्त (बेनियाज़) हो जाओ तो लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : ईश्वर किसी से प्रेम करे और इसके साथ ही वह लोकप्रिय भी हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का बताया हुआ कार्य जिसको करने के बाद कोई व्यक्ति ईश्वर और उसके बन्दों का प्रिय बन जाता है, गहरे मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। दुनिया से अनासक्त हो जाने के बाद आदमी पूर्णतया ईश्वर के लिए फ़ारिग़ हो जाता है। उसकी सारी दिलचस्पियाँ ईश्वर के लिए ख़ास हो जाती हैं। उसके यहाँ ईश्वर का प्रेम और पारलौकिक कामनाएँ इतनी प्रबल होती हैं जो उसके जीवन को श्रेष्ठतर और अर्थमय बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं। ज़ाहिर है ऐसा व्यक्ति ईश्वर का प्रिय हो जाएगा। जो ईश्वर का हो गया, अनिवार्यतः ईश्वर भी उसका हो जाएगा।
इसी प्रकार आदमी जब लोगों की धन-सम्पत्ति और उनकी दूसरी चीज़ों के प्रति अनासक्त (बेनियाज़) हो जाता है और लोगों से वह कोई आशा और लालच नहीं रखता तो लोगों की निगाहों में उसका वज़न बढ़ जाता है। लोग मजबूर होते हैं कि उसे अपने दिल में जगह दें। ऐसा व्यक्ति लोगों से सम्बन्ध-विच्छेद तो नहीं करता, किन्तु वह लोगों से मिलता है तो अपने किसी व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि वह इसे लोगों का एक हक़ समझता है कि उनसे सम्बन्ध बनाए रखे। उसके सम्बन्ध लोभ-लालच और स्वार्थपरता आदि से सर्वथा मुक्त होते हैं। वह लोगों से स्वयं उन्हीं के लिए मिलता है। लोगों की भलाई उसके समक्ष होती है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति असाधारण महत्व प्राप्त कर लेगा। उसके व्यक्तित्व में बड़ा सौन्दर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा।
(2) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब अपने पिता से और वे अपने दादा अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इस उम्मत का सबसे पहला सुधार और भलाई विश्वास और अनासक्ति है और इसका सबसे पहला बिगाड़ और ख़राबी कृपणता और आशा एवं दीर्घ कामना है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : मुस्लिम समुदाय का कल्याण और सफलता जिन चीज़ों पर निर्भर करती है उनमें विश्वास और अनासक्ति को मौलिक महत्व प्राप्त है। ये वे विशिष्ट गुण हैं जो इस समुदाय को दुनिया के दूसरे समुदायों और क़ौमों में विशिष्टता प्रदान करते हैं। इस उम्मत को विश्वास की शक्ति दी गई है। जो चीज़ें आम निगाहों को दिखाई देती हैं उनसे कहीं ज़्यादा इस उम्मत का भरोसा और विश्वास उसपर होता है जिसको आम निगाहें नहीं देखतीं। ईमान रखनेवालों को इसका भान होता है कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। सब कुछ उसी के हाथ में है। वह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसलिए उनका अस्ल भरोसा अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वरीय सत्ता पर होता है। क़ुरआन में है—
"कहो, ऐ बादशाही के मालिक! तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे प्रतिष्ठा दे और जिसे चाहे अपमानित कर दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तुझे प्रत्येक चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।" (3:26)
इस समुदाय की दूसरी विशिष्टता वह है जिसे इस हदीस में अनासक्ति (बेनियाज़ी) कहा गया है। अनासक्ति का अर्थ यह है कि आदमी निरुत्साहित न हो, अपनी निगाह को बुलन्द रखे और दुनिया और उसके अस्थायी सुख और चैन को अपना लक्ष्य न बनाए। विश्वास और अनासक्ति का गुण वास्तव में अगर किसी क़ौम में पैदा हो जाए तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान करना कठिन होगा। वह क़ौम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ी से बड़ी क़ुरबानी पेश करने से नहीं रुक सकती। लक्ष्य के लिए प्राणों और धन-सम्पत्ति को क़ुरबान करना उसके लिए एक आसान बात होगी।
लेकिन यह मौलिक विशिष्टता अगर मुस्लिम समुदाय में शेष न रहे तो फिर उसे पस्ती और बिगाड़ से कोई भी चीज़ बचा नहीं सकती। विश्वास की शक्ति और संयम के गुण के अभाव में उसके अन्दर कृपणता और दीर्घ आशाओं का पैदा होना अनिवार्य है। आदमी माल ख़र्च करने के बजाय माल समेटने की चिन्ता में ग्रस्त होगा। सत्यमार्ग में जान देने के बजाय वह दुनिया में अधिक से अधिक जीने का लोभी होगा। उसके लोभ-लालच का कोई अन्त न होगा। वह दुनिया में अधिक-से-अधिक जीवित रहने और उससे लाभ उठाने का अभिलाषी होगा। वह ईश्वर को भूल जाएगा। उसकी आशाएँ दुनिया ही से सम्बद्ध होकर रह जाएँगी। कृपणता और दीर्घ आशा ने जहाँ दिलों में घर किया, ईमान वाले अपने उच्च स्थान से गिरते ही जाएँगे। कोई चीज़ न होगी जो उन्हें उनके बुरे अंजाम से बचा सके।
(3) हज़रत अबू-ज़र-ग़िफ़ारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"दुनिया के प्रति अनासक्ति (बेनियाज़ी) यह नहीं है कि वैध को अपने लिए अवैध कर लिया जाए और माल को नष्ट किया जाए। बल्कि दुनिया के प्रति अनासक्ति यह है कि जो कुछ तुम्हारे हाथों में हो उससे कहीं अधिक भरोसा तुम्हें उसपर हो जो ईश्वर के हाथों में है। और यह कि तुम्हें जो कष्ट और तकलीफ़ पहुँचे तो (ईश्वर के यहाँ मिलनेवाला) उसका प्रतिदान तुम्हें इतना रुचिकर हो कि तुम इसकी इच्छा करो कि काश यह मुसीबत बाक़ी रहे!" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में अनासक्ति की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है और अनासक्ति के विषय में अनभिज्ञ लोगों की धारणा के विचार का सुधार किया गया है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन से ज्ञात हुआ कि अनासक्ति का मूल सम्बन्ध आदमी की मानसिकता और उसके दृष्टिकोण से है। अनासक्ति का अर्थ यह हरगिज़ नहीं होता कि आदमी ईश्वर की उन नेमतों और उसकी प्रदान की हुई उन राहतों को अपने ऊपर हराम कर ले जिनको उसने इनसानों के लिए वैध कर रखा है। उदाहरणार्थ अच्छा खाना-पीना, आराम और राहत, शादी-विवाह आदि। बल्कि अनासक्ति यह है कि आदमी दुनिया और दुनिया की अस्थायी चीज़ों पर भरोसा न करे। उसके समक्ष आख़िरत का स्थायी सुख-चैन और ईश्वर का वह पुरस्कार हो जिसका उससे उसके रब ने वादा किया है। उसकी दृष्टि ईश्वर के शाश्वत अलौकिक ख़ज़ानों पर हो। ईश्वरीय अनुग्रह और अनुकम्पा पर उसे पूर्ण भरोसा और विश्वास हो। दुनिया में वह विपत्तियों और परीक्षाओं की कामना न करे, बल्कि ईश्वर से निश्चिन्तता और सुख-चैन की माँग ही करता रहे। और अगर ईश्वर के आदेश से किसी विपत्ति का उसे सामना करना पड़ जाए तो उस विपत्ति का जो प्रतिदान ईश्वर के यहाँ उसे मिलनेवाला है, उसके मुक़ाबले में वह उस विपत्ति को तुच्छ समझे। किसी विपत्ति का सामना न होने के मुक़ाबले में ईश्वर के यहाँ उस विपत्ति के बदले में दिया जानेवाला प्रतिदान उसे कहीं अधिक प्रिय हो।
(4) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस बन्दे ने संसार के प्रति अनासक्ति की नीति अपनाई, अनिवार्यतः ईश्वर ने उसके हृदय को तत्वदर्शिता प्रदान की और उसकी ज़बान से तत्वज्ञान की बातें जारी कर दीं और दुनिया का दोष और रोग उसपर स्पष्ट कर दिया और उसका उपचार भी उसे सुझा दिया, और फिर स्वस्थ और भला-चंगा उसे दुनिया से निकालकर सलामती के घर की ओर ले गया।" (हदीस : बैहक़ी फ़ी शोअ्बिल ईमान)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि अनासक्ति की नीति अपनानेवाला घाटे का सौदा नहीं करता। आख़िरत में तो उसे सफलता प्राप्त होगी ही जिसे दृष्टि में रखकर उसने सांसारिक सुख और भोग-विलास को तुच्छ समझा, इस दुनिया में भी ऐसे व्यक्ति के हिस्से में 'ख़ैरे-कसीर' (महाधन) आता है। अनासक्ति के कारण उसकी हृदय भूमि बुद्धिमत्ता और तत्वदर्शिता की कृषि भूमि बन जाती है और उसके मुख से जो बातें निकलती हैं वे तत्वदर्शिता से परिपूर्ण होती हैं। उसकी बातें सतही और साधारण नहीं होतीं, बल्कि वे ज्ञान और विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ईश्वर उसे दुनिया के दोषों और उसके रोगों और उसके फ़ितनों आदि से अवगत करा देता है और उसे ऐसी समझ और अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है कि वह उन ख़राबियों और फ़ितनों का सफलतापूर्वक मुक़ाबला करता और अपने आपको उनसे सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त करता है। फिर जब वह इस नश्वर जगत् से विदा होकर आख़िरत के स्थायी घर की ओर रवाना होता है तो वह हर प्रकार की कलुषताओं और ख़राबियों से मुक्त होता है। उसकी प्रकृति और स्वभाव में निर्मलता और शुद्धता होती है। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसका सब कुछ तबाह हो गया।। क़ुरआन में है—
“जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, सिवाय इसके कि कोई भला-चंगा हृदय लेकर ईश्वर के समक्ष उपस्थित हुआ हो।” (26:89)
बेनियाज़ी
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“धनवान होने का सम्बन्ध धन-सम्पत्ति के बाहुल्य से नहीं। धनी होना तो हृदय के धनी होने पर निर्भर करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में जिस चीज़ की तलाश में है वह है सुख-शान्ति और हार्दिक सन्तोष। कोई इसे सांसारिक धन-सम्पत्ति और वैभव में पाने की उम्मीद रखता है और कोई इसे प्रसिद्धि और नामवरी में ढूँढता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने से अपरिचित होकर अपेक्षित चीज़ को बाह्य जगत् में तलाश कर रहा है, हालांकि हार्दिक सन्तोष का रहस्य वास्तव में स्वयं अपने आपको पाने में निहित है। किसी ने अगर सम्पूर्ण सांसारिक वैभव जुटा लिया लेकिन स्वयं का अन्वेषण न कर सका या मात्र सांसारिक धन-सम्पत्ति की प्राप्ति में स्वयं को गँवा बैठा तो उसे हार्दिक सन्तोष का धन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसे हार्दिक परितोष प्राप्त है वास्तव में धनवान और समृद्ध वही है।
आदमी का असल और बड़ा हिस्सा वह है जो आँखों से दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखाई देता है वह बहुत थोड़ा है और उसका शेष रहना भी उसी पर निर्भर है जो दिखाई नहीं देता। इसलिए आवश्यक है कि आदमी अपने अन्तर्जगत और हृदय को धनी बनाए। अगर वह सोचता है कि भौतिक सुख-सामग्रियों की प्राप्ति उसे तृप्त करेगी तो यह उसकी बुनियादी ग़लती है। तृप्ति और सन्तोष का वास्तविक सम्बन्ध हृदय से है। अगर किसी ने अपने आत्म (Self) को पहचान लिया और ईश्वर के मार्गदर्शन में उसे पूर्णत्व की ओर ले गया तो उससे बढ़कर धनी कोई और नहीं। दृष्टिवान सत्य को पा लेते हैं और उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उन्हें जो तृप्ति, शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है, सामान्य स्थिति में उसका अन्दाज़ा करना भी असम्भव है। इमाम इब्ने-तैमिया कहते हैं—
“मेरी जन्नत मेरे सीने में है। मैं जहाँ भी रहूँगा मेरी जन्नत मेरे साथ होगी।”
इस जन्नत से उनका अभिप्राय हार्दिक परितोष और ईमान का माधुर्य ही है। जो हृदय के धनी होते हैं उनके स्वभाव में अत्यन्त सादगी आ जाती है। न वे सांसारिक धन-दौलत के भूखे होते हैं और न उनको उन चीज़ों की आरज़ूएँ ही सताती हैं जिनके पीछे सांसारिक लोग दौड़ते रहते हैं। वे जीवन के उस सूक्ष्म और कोमल स्वभाव से परिचित हो जाते हैं जिससे बढ़कर बहुमूल्य कोई रत्न नहीं।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति की नीयत (कर्मों में) आख़िरत चाहने की हो, ईश्वर उसे हार्दिक सम्पन्नता देता है और बिखरने से बचाकर उसे परितोष प्रदान करता है। दुनिया उसके पास आती है और वह उसकी दृष्टि में तुच्छ और मूल्यहीन होती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की नीयत (कर्मों में) दुनिया चाहने की हो, ईश्वर दरिद्रता को उसकी आँखों के सामने कर देता है। उसके काम में बिखराव और परेशानी डाल देता है और इस सबके बावजूद दुनिया उसे बस उतनी ही मिलती है जो उसके लिए निश्चित होती है।" (हदीस : तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, दारमी)
व्याख्या : बेनियाज़ी के सम्बन्ध में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण हदीस है। यह हदीस बताती है कि बेनियाज़ी की दौलत उस समय तक किसी को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह दुनिया का चाहनेवाला बनने के बजाय आख़िरत का चाहनेवाला बनकर जीवन व्यतीत न करने लगे। आख़िरत की कामना वास्तव में हमारी समस्त मानसिक और वैचारिक परेशानियों और उलझनों का इलाज है। आख़िरत की कामना से मनुष्य को वह शान्ति और परितोष प्राप्त होता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया जो पतनोन्मुख, सीमित और छुद्र है, उसपर मोहित होना अपनी मानसिक शान्ति और सुख-चैन को ग़ारत करना है। चाहने की चीज़ तो परलोक ही है। दुनिया का इच्छुक सदैव दरिद्रता के भय से ग्रस्त रहता है। उसका मामला कभी दुरुस्त नहीं होता। बिखराव और परेशानी ही उसका जीवन होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आख़िरत को सदैव अपनी दृष्टि में रखता है, ईश्वर उसे नक़द इनाम अता करता है कि उसके दिल को बेनियाज़ी प्रदान करता है जो जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।
स्वच्छ हृदय
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे साथियों में से कोई व्यक्ति मुझ तक किसी की कोई बात न पहुँचाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल साफ़ हो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि दूसरों के प्रति अपने हृदय को स्वच्छ और साफ़ रखना अभीष्ट और प्रशंसित है। हृदय की स्वस्थता और निर्मलता के लिए अनिवार्य है कि किसी के सम्बन्ध में अनावश्यक बातों के सुनने से परहेज़ किया जाए। हृदय चाहे कितना ही स्वच्छ और पवित्र क्यों न हो, उसके दूषित होने की आशंका निरन्तर बनी रहती है। दूसरों के बारे में ऐसी बातें जानने का शौक़ अत्यन्त अप्रिय है जिनसे हृदय में दुर्भावनाओं और वैमनस्य के उत्पन्न होने की सम्भावना हो। अलबत्ता वे अवसर इसके अपवाद हैं जहाँ धार्मिक ज़रूरत और अपनी मस्लहत के कारण यह अपरिहार्य हो जाता है कि किसी के विषय में कुछ कहा या सुना जाए।
भरोसा
(1) हज़रत उमर-बिन-ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“अगर तुम ईश्वर पर ऐसा भरोसा करो जैसा कि उसपर भरोसा करने का हक़ है तो वह तुम्हें इस तरह आजीविका दे जिस तरह कि वह पक्षियों को देता है। वे सुबह को भूखे अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस होते हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : इस हदीस को समझने के लिए क़ुरआन की ये आयतें भी दृष्टि में रहनी चाहिएँ—
“धरती में चलने-फिरनेवाला जो प्राणी भी है उसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है।" (11:6)
“कितने ही चलने-फिरनेवाले जीवधारी हैं जो अपनी आजीविका उठाए हुए नहीं फिरते, अल्लाह ही उन्हें आजीविका देता है और तुम्हें भी। वह सब कुछ सुनता, जानता है।" (29:60)
इंजील मत्ती में हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) का यह कथन उद्धृत है : "मैं तुम से कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएँगे अथवा क्या पीएँगे। और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो! वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न कोठियों में जमा करते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा महत्व उनसे अधिक नहीं है?
और तुममें कौन ऐसा मनुष्य है जो चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम वस्त्र के लिए क्यों चिन्ता करते हो? जंगली सोसन के पेड़ों को ध्यान से देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं? वे न परिश्रम करते हैं और न कातते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, सुलैमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान सुन्दर राजसी वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा भव्य वस्त्र पहनाता है तो ऐ अल्पविश्वासियो, तुमको वह क्यों न पहनाएगा?
इसलिए तुम चिन्ता मत करना और यह न कहना कि हम क्या खाएँगे? क्या पीएँगे? क्या पहनेंगे? अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएँ चाहिएँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएँ भी तुम्हें मिल जाएँगी।
कल के लिए चिन्ता न करो; क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है।" (मत्ती, 6:25-34)
हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) का इसी प्रकार का एक भाषण लूक़ा (12:22-34) में भी मिलता है।
उपरोक्त हदीस, क़ुरआन की आयतों और हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) के कथनों से मालूम होता है कि ईश्वर अपने आज्ञाकारी बन्दों का मित्र और कारसाज़ है। वह उनका संरक्षक है। वह उनकी आवश्यकताओं को भली-भाँति समझता है। वह उन्हें अनाथों की तरह बेकसी और बेबसी की हालत में हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। वह दुनिया में उनकी आवश्यकताएँ और कामनाएँ पूरी करता है। केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं, वह तो अपने वफ़ादारों को ऐसा जीवन प्रदान करता है जो अत्यन्त पवित्र और सुन्दर होता है। न उनका वर्तमान जीवन प्रकाशरहित होता है और न उनका भविष्य अन्धकारमय। वे मर्मज्ञ होते हैं। उनका वास्तविक उपार्जन यह होता है कि वे ईश-भक्ति पर आधारित पवित्र जीवन का आस्वादन कर रहे होते हैं। वे पवित्र और वैध आजीविका की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनका असल भरोसा अपने प्रयास पर नहीं, बल्कि अपने ईश्वर पर होता है।
(2) हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी के दिल के लिए प्रत्येक घाटी में एक शाखा और कोना है, अब जिस व्यक्ति ने अपने दिल को उन शाखाओं से लगाए रखा तो ईश्वर को बिलकुल इसकी चिन्ता न होगी कि कौन-सी घाटी उसे तबाह और बरबाद करती है। और जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करेगा तो ईश्वर इसके लिए पर्याप्त होगा कि उसे उन घाटियों में भटकते रहने से बचा ले।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : आदमी की अन्धी वासनाएँ उसे प्रत्येक घाटी में लिए फिरती हैं। वह हर जगह अपने लिए आकर्षण महसूस करता है। अब जो व्यक्ति उन वासनाओं को ही अपना मार्गदर्शक बनाकर उनके पीछे दौड़ता और प्रत्येक घाटी में भटकता फिरता है, ईश्वर को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि ऐसा व्यक्ति कहाँ और तबाही के किस गड्ढे में दम तोड़ता है। इसके विपरीत जो लोग अपनी आवश्यकताओं और कामनाओं के सिलसिले में अपने को वासनाओं और अन्धी इच्छाओं के हवाले करने के बजाय ईश्वर के मार्गदर्शन को अपना रहनुमा बनाते हैं तो ईश्वर न केवल यह कि ऐसे लोगों को प्रत्येक प्रकार की तबाही से बचा लेता है, बल्कि वह उन्हें एकाग्रता और हार्दिक परितोष भी प्रदान करता है और उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ऊँटनी को बाँधकर (अल्लाह पर) भरोसा करूँ या उसे छोड़कर भरोसा करूँ? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "उसे बाँधो, फिर भरोसा करो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मालूम हुआ कि ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आदमी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और इस इन्तिज़ार में रहे कि उसके लिए ईश्वर की ओर से सारी व्यवस्था हो जाएगी। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह ईश्वरप्रदत्त साधनों को काम में लाए और परिणाम को ईश्वर के हवाले कर दे। यही ईश्वर पर भरोसा करना है। देता ख़ुदा ही है लेकिन उसके देने में पर्दादारी की एक शान पाई जाती है। पर्दादारी की इस नीति का आदर आवश्यक है। आदमी सारे ही साधनों को काम में लाए लेकिन अस्ल भरोसा उसका ईश्वर ही पर हो। ईश्वर पर भरोसा करना वास्तव में उस विशिष्ट सम्बन्ध को व्यक्त करता है जो मोमिन का अपने ईश्वर से होना चाहिए। अतएव क़ुरआन में आया है—
“और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।" (9:51)
एक और जगह कहा गया—
“और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो निश्चय ही अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है।" (8:49)
अर्थात उसके लिए बन्दे का काम बना देना कुछ भी मुश्किल नहीं।
आज्ञाकारिता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि तुम्हारे प्रतापवान प्रभु का कथन है कि—
“अगर मेरे बन्दे मेरे आज्ञाकारी बनें तो मैं उनपर रात को वर्षा करुँ और दिन में उनपर धूप निकालूँ और उन्हें बिजली की कड़क की आवाज़ न सुनाऊँ।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात जब रात में वे सो रहे होंगे, हम वर्षा कराएँगे ताकि वे सुकून से सोएँ और उनकी खेतियाँ सिंचित हों। बादल की गरज और कड़क से भी उन्हें सुरक्षित रखें ताकि वे भयग्रस्त न हों और उन्हें कोई हानि न पहुँचे। दिन के समय धूप निकाल दें ताकि वे अपने कामों में व्यस्त हो सकें।
यह हदीस बताती है कि बन्दगी और आज्ञापालन के फ़ायदे दुनिया के जीवन में भी ज़ाहिर होते हैं। क़ुरआन में भी है—
“अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और ईश-परायण होते तो अनिवार्यतः हम उनपर आकाशों और धरती की बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुठलाया, तो जो कुछ कमाई वे करते थे उसके बदले में हमने उन्हें पकड़ लिया।" (7:96)
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"इनकार करनेवाला जब नेक कर्म करता है तो इसके कारण दुनिया की रोज़ी और ख़ुराक में उसके लिए कुछ कुशादगी हो जाती है। रहा ईमान लानेवाला व्यक्ति, तो अल्लाह उसकी नेकियों को आख़िरत की ख़ातिर उसके लिए जमा करके रखता है और उसके बाद दुनिया में भी उसके आज्ञापालन पर उसे आजीविका प्रदान करता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि अगर ईश्वर का इनकार करनेवाले व्यक्ति के कुछ नेक कर्म हैं तो उनका बदला उसे दुनिया ही में चुका दिया जाता है। आख़िरत में उसके हिस्से में यातना के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन ईमानवाले का मामला इससे बिलकुल भिन्न है। ईश्वर मोमिन के नेक कर्मों को जमा करता रहता है। आख़िरत में वह उसे उनका प्रतिदान देगा। मगर इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि मोमिन का जीवन दुनिया में अभावग्रस्त होता है और उसके आज्ञापालन और बन्दगी का प्रभाव और परिणाम केवल आख़िरत में सामने आएगा। दुनिया में भी आज्ञाकारिता अपना प्रभाव दिखाती है। यहाँ भी ईश्वर इसके कारण उसे आजीविका प्रदान करता है।
परितोष
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सफल हो गया वह व्यक्ति जिसने इस्लाम अपनाया, आजीविका भी उसे आवश्यकतानुसार मिली, और ईश्वर ने उसे जो कुछ प्रदान किया उस पर उसे सन्तुष्ट भी बना दिया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इससे बढ़कर कल्याण और सफलता की बात क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को अपना प्रभु और शासक मानकर उसके आगे अपने को झुका दे। ईश्वर ने उसे ज़रूरत के अनुसार आजीविका भी दी और उसपर उसे सन्तुष्टि भी प्रदान की, हालांकि इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म और विश्वास की ख़ातिर उसे अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता या कम से कम उसे मुसीबतों, भूख और दरिद्रता का शिकार होना पड़ता। अगर वह परितोष-धन से वंचित होता तो सम्भव था कि वह दुखी हो जाता कि उसे प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त नहीं। मगर ईश्वर की दी हुई आजीविका पर सन्तुष्ट होने के कारण वह किसी दुख में ग्रस्त नहीं हो सकता। ईमान और इस्लाम के बाद जिस व्यक्ति को परितोष धन प्राप्त हुआ हो, उसे तो ईमान और आज्ञाकारिता की भावना से रहित मनुष्य ही दरिद्र प्रतीत होगा, चाहे वह कितने ही बड़े ख़ज़ाने का मालिक क्यों न हो।
सुरुचि
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी अहंकार होगा।” एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी चाहता है कि उसका वस्त्र अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। (क्या यह भी अहंकार में सम्मिलित है?) कहा, "अल्लाह सुन्दर है। और सौन्दर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो यह है कि सत्य को असत्य ठहराया जाए और लोगों को तुच्छ और क्षुद्र समझा जाए।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर अपने अस्तित्त्व, गुण और कर्म आदि प्रत्येक दृष्टि से सौन्दर्यवान है और सुन्दरता उसे प्रिय है, इसलिए सुन्दर कपड़े और अच्छे जूते पहनना अहंकार नहीं है। ईश्वर तो चाहता है कि आदमी प्रत्येक मामले में सुन्दरता का ध्यान रखे। कुरूपता और बेढंगेपन को वह कैसे पसन्द कर सकता है, अलबत्ता लोगों को दिखाने और उनपर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अगर कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो निस्सन्देह यह अहंकार है। मनुष्य अगर अहंकारी नहीं है तो लोगों के सामने ही नहीं, एकान्त में भी वह सौन्दर्य का ध्यान रखेगा और सँवरा हुआ ही रहेगा। अगर अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे तरीक़े से रहने में अपनी सुरुचि के अतिरिक्त किसी की दृष्टि में यह भी हो कि इससे दूसरों को भी एक प्रकार की प्रसन्नता होगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छी आवाज़ में क़ुरआन पढ़ता है और समझता है कि ईश्वर प्रसन्न होगा और श्रोताओं के हृदय भी इससे आनन्दित होंगे तो यह दिखावा नहीं। सौन्दर्य वास्तव में अत्यन्त बढ़ी हुई सुन्दरता को कहते हैं जो सर्वथा सन्तुलित हो। सौन्दर्य का सम्बन्ध बाह्य और अन्तर, व्यवहार और नैतिकता हरेक से है। अतएव क़ुरआन में है—
“रहे जानवर, उन्हें भी उसी ने पैदा किया है जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान भी है, और दूसरे कितने ही फ़ायदे हैं, और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो, उनमें तुम्हारे लिए सौन्दर्य भी है, जबकि तुम शाम के समय उन्हें लाते हो और जैसा कि तुम उन्हें चराने ले जाते हो।” (16:5-6)
एक दूसरे स्थान पर क़ुरआन में आया है—
“उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारे जी ने बहकाकर तुम्हारे लिए एक बात बना दी है। अब धैर्य ही उत्तम और सुन्दर है।" (12:18)
मालूम हुआ कि धैर्य जो एक नैतिक चीज़ है, सौन्दर्य का सम्बन्ध उससे भी है। इसी प्रकार और भी आयतें हैं, उदाहरणार्थ—
“और जो कुछ वे कहते हैं उसपर धैर्य रखो, और सुन्दरता के साथ उन्हें छोड़ दो।" (73:10)
“और वह क़ियामत की घड़ी तो अनिवार्यतः आने वाली है। अतः तुम भली प्रकार दरगुज़र (क्षमा) से काम लो।" (15:85)
“ऐ नबी अपनी पत्नियों से कह दो कि अगर तुम सांसारिक जीवन और उसकी साज-सज्जा चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे-दिलाकर भली रीति से विदा कर दूँ।" (33:28)
ये आयतें इस बात का प्रमाण हैं कि धैर्य ही में नहीं, किसी से अलग होने, दरगुज़र से काम लेने और किसी को विदा करने में भी सौन्दर्य पाया जा सकता है। इस्लाम की विशिष्टता यह है कि उसने सारे ही मामलों में सौन्दर्य का ध्यान रखा है। सौन्दर्य में सन्तुलन, विविधता, संग्राहकता, पवित्रता, माधुर्य, आनन्द, सुख और शीतलता— सब कुछ मौजूद होने की सम्भावना रहती है। इस्लाम अरुचि, संवेदनहीनता, शुष्कता और जड़ता का धर्म हरगिज़ नहीं है। हम देखते हैं कि सहाबा शुष्क स्वभाव के न थे। वे सही अर्थों में जीवन का मूल्य पहचानते थे और अपने जीवन में इस्लामी सभ्यता और शिष्टता का पूरा ध्यान रखते थे। उनके बारे में यह हदीस मौजूद है—
“हज़रत क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पूछा गया कि क्या अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा हँसते थे? उन्होंने कहा, "हाँ, लेकिन इसके साथ ही ईमान उनके हृदयों में पर्वत से भी ज़्यादा मज़बूत था।" बिलाल-बिन-साद कहते हैं कि मैंने उन्हें तीरों के निशाने पर दौड़ते देखा है, इस हाल में कि उनमें से कुछ लोग कुछ लोगों से हँसी-मज़ाक़ कर रहे होते थे। फिर जब रात होती तो वे संन्यासी और बैरागी बन जाते थे।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
मतलब यह है कि वे अपने रसूल की दी हुई सूचनाओं पर इस तरह ईमान रखते थे जैसे किसी ने सामने के पर्वत को, बल्कि उससे भी स्पष्टतर और महानतर चीज़ को स्वीकार किया हो। वे कोई शुष्क लोग न थे। उनके ईमान ने उनके स्वभाव को विकृत और हताहत नहीं किया था। उन्होंने ईमान को सहज और स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया था। उनका ईमान शिथिल और उदासीन न था, हालाँकि उनका ईमान पर्वत से भी अधिक वज़नी था जिसे वे उठाए हुए थे। वे दौड़ते और परस्पर प्रतिस्पर्धा और हास्य-विनोद भी करते थे। इसलिए कि यह सामूहिक, जीवनयापन की एक स्वाभाविक अपेक्षा थी। उनके समाज में कृत्रिमता न थी। उनकी स्वाभाविक सादगी ने उनके रहन-सहन को आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक और मनोरम बना दिया था। वे लोगों के मध्य कोरे संन्यासी बनकर नहीं बल्कि अपनी सम्पूर्ण जीवन्तता के साथ रहते थे। वे अपने ईमान और इस प्रकार के जीवन में कोई विरोध महसूस नहीं करते थे। उनका ईमान उस बीज की भाँति था जिसने एक सदाबहार जीवनवृक्ष का रूप ले लिया था। उनका ईमान कोई पर्णहरित सूखा वृक्ष न था जिसमें न फूल खिलते हों और न कोई ख़ुशबू पाई जाती हो। जब रात्रि आकर इस प्रत्यक्ष लोक पर अपना आवरण डाल देती, संसार की सारी वस्तुएँ निगाहों से ओझल हो जातीं, मित्र और सहचर अपने घरों की राह लेते, उस समय वे महसूस करते कि वह सत्ता जो जीवन और जगत् का आदिस्रोत है, अब हम उसके सम्मुख हैं तो उनका सारा ध्यान सहज ही उसकी ओर केन्द्रित हो जाता और वे अत्यन्त आदरसूचक मुद्रा में हो जाते। ईश-भय उनके हृदय में और भी गहरा हो उठता। वे अपने रुकूअ और सज्दों के द्वारा उसके समक्ष अपना दास्यभाव प्रकट करते और उसे राज़ी करने के लिए प्रयासरत हो जाते।
मानो वे प्रत्येक सन्दर्भ और प्रसंग में अपेक्षित व्यवहार को भली-भाँति समझते थे। यही अल्लाह के रसूल की सुन्नत (रीति) भी थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में आता है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) परिवार जनों से वार्तालाप कर रहे होते थे किन्तु नमाज़ का समय होते ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हाल यह होता कि मानो किसी को पहचानते ही नहीं हैं, और फिर आप मस्जिद में नमाज़ के लिए चल पड़ते। सम्भव न था कि कोई चीज़ आपको ईश्वर की सेवा में उपस्थित होने से रोक दे।
शुद्धता और निर्मलता
(1) हज़रत अबू-मालिक अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"सफ़ाई आधा ईमान है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में इस वास्तविकता की ओर इशारा किया गया है कि ईमान सर्वथा पवित्रता और स्वच्छता है। यह मन की पवित्रता के नतीजे में प्राप्त होता और शेष रहता है। इसकी अभिव्यक्ति भी सदैव पवित्रता लिए हुए होती है। ईमान की माँग यह है कि हमारा बाह्य और अन्तर दोनों ही पवित्र हों। न हमारा बाह्य अपवित्र हो और न अन्तर। हमारा जीवन अपने आन्तरिक और बाह्य दोनों पहलुओं से पवित्र हो। क़ुरआन ने बहुदेववादियों को अपवित्र इसी लिए कहा है कि वे प्रत्यक्ष रूप से कितना ही पवित्र और स्वच्छ रहने का प्रयास करते हों लेकिन उनका अन्तर सदैव अपवित्र ही रहता है। (हदीस : क़ुरआन, 9:28)
एक व्यक्ति अगर अपने शरीर, परिधान, घर, दरवाज़े आदि सभी को साफ़ रखता है तो मानो उसने ईमान के आधे तक़ाज़े को पूरा कर लिया। आधा ईमान उसके हिस्से में आ गया। और अगर अपने बाह्य पक्ष के साथ उसने आन्तरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखा है, वह न तो बहुदेववाद के निकट जाता है और न कभी अपने हृदय को ईश्वर की महानता और उसके पूजनीय और प्रिय होने के एहसास से ख़ाली होने देता है, हृदय में ईर्ष्या, स्वार्थपरता, द्वेष, अहंकार आदि को भी जगह नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि ईमान के शेष आधे तक़ाज़ों की ओर से भी वह ग़ाफ़िल नहीं है। उसे आधा नहीं बल्कि पूरा ईमान हासिल है।
(2) हज़रत मुआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन लानत के कामों से बचो, और वे ये हैं— मलत्याग करना नदी के घाटों पर, रास्ते में और छायादार स्थान पर।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहाँ सामान्यतः लोगों का आना-जाना रहता है। इन स्थानों को मलत्याग कर गन्दा करने से लोगों को जो तकलीफ़ होगी उसका अनुमान प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। लोगों को कष्ट पहुँचाना अत्यन्त अधमता और कमीनेपन का काम है। फिर इन स्थानों पर मलत्याग के लिए बैठना निर्लज्जता की बात भी है। इससे घिन आती है। इन स्थानों (Public Places) पर मलत्याग करनेवाले को लानत का भागी क़रार देकर सचेत किया गया है कि यह हरकत ईश्वर की दृष्टि में अत्यन्त घृणित है। इससे बचना चाहिए।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दायाँ हाथ वुज़ू और खाना खाने में इस्तेमाल करते थे और बाएँ हाथ से शौच और इस जैसे कार्य करते थे।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह पवित्रता और स्वभाव की स्वच्छता का तक़ाज़ा है कि पवित्र कार्य दाएँ हाथ से किए जाएँ। दूसरे कार्य जैसे दीर्घशंका से निवृत्त होकर पानी से सफ़ाई करना, नाक साफ़ करना, आदि बाएँ हाथ से किए जाएँ।
(4) हज़रत मुआविया-बिन-क़ुर्रा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इन दो वनस्पतियों— लहसुन और प्याज़ से मना किया है और कहा है कि "जो व्यक्ति इन्हें खाए वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए।" और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अगर उनका खाना अपरिहार्य हो तो पकाकर उनकी गन्ध को समाप्त कर देना चाहिए।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह नफ़ासत और पवित्रता का तक़ाज़ा है कि दुर्गन्धित चीज़ों के खाने में एहतियात से काम लिया जाए। ऐसी चीज़ें खाकर किसी मजलिस या मस्जिद में तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को कष्ट पहुँचेगा।
यह हदीस बताती है कि इस्लाम में स्वच्छता और पवित्रता का कितना ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि सामूहिक आचार में इसे सम्मिलित कर दिया गया है।
धर्म में किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं रखी गई है। इसी लिए कहा गया कि अगर प्याज़ और लहसुन खाना किसी कारणवश ज़रूरी हो तो उनको पकाकर खाया जाए ताकि उनकी गन्ध समाप्त हो जाए।
स्वस्थ स्वभाव
(1) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति ईश्वर की दी हुई थोड़ी-सी आजीविका पर राज़ी हो जाए तो ईश्वर भी उसके थोड़े-से कर्म पर राज़ी हो जाता है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : ईश्वर के यहाँ वास्तव में जिस चीज़ का महत्व है वह है बन्दे के स्वभाव की स्वस्थता और निर्मलता। अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति में टेढ़ है तो उसके बड़े-से-बड़े कारनामों की भी ईश्वर की दृष्टि में कोई क़ीमत नहीं है, लेकिन आदमी अगर किसी क़िस्म के दिखावे में लिप्त नहीं है, न उसके अन्दर कोई टेढ़ पाई जाती है और न उसकी प्रवृत्ति में कोई ख़राबी है तो वह अपने लिए तो सबसे मूल्यवान और आनन्ददायक निधि इसको समझेगा कि अल्लाह उसका प्रभु है। इसके बाद जीवन में दूसरी चीज़ों की कमी-बेशी का उसकी दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। अगर किसी व्यक्ति में यह बात पैदा हो गई तो समझ लीजिए कि उसका हृदय स्वस्थ और निर्मल है। स्वस्थ हृदय और निर्मल स्वभाव हमें प्राप्त है या नहीं इसकी एक ऐसी पहचान इस हदीस में बताई गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है।
किसी व्यक्ति को अगर दुनिया में थोड़ी आजीविका मिली और वह उसपर राज़ी रहा, कोई शिकायत उसे नहीं हुई तो यह उसके अन्तर की पवित्रता और हृदय की निर्मलता और स्वस्थता का स्पष्ट प्रमाण है। अनिवार्यतः ईश्वर उससे प्रसन्न होगा चाहे दुनिया के जीवन में वह बहुत अधिक कर्म न कर सका हो। उसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जिससे प्रत्येक कमी पूरी हो जाती है। इस गुण से अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो इसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कर्म के द्वारा सम्भव नहीं।
प्रसन्नता और आनन्द
(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा कि ईमान क्या है? रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “जब तुझे अपनी नेकी से प्रसन्नता और अपने बुरे काम से दुख हो तो तू मोमिन है।" उसने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! गुनाह क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "जब कोई चीज़ तेरे दिल में दुविधा और खटक पैदा करे तो उसे छोड़ दे।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : ईमान के विषय में प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह है कि ईमान की पहचान और उसका लक्षण क्या है? हम किस तरह समझें कि हमारा दिल ईमान के भाव से रिक्त नहीं है।
इस हदीस से मालूम हुआ कि ईमान की पहचान यह है कि नेकी करके तुझे प्रसन्नता हो। ईमान का सम्बन्ध बुराई से नहीं, नेकी से होता है। ईमान का तक़ाज़ा ही यह है कि आदमी जीवन में नेक कर्म करे। स्वयं ईमान शान्ति और आनन्द प्रदान करता है, वह कोई अप्रिय चीज़ नहीं है। इसलिए जब ईमान के तक़ाज़े पूरे होंगे तो आदमी की प्रसन्नता और आनन्द में वृद्धि ही होगी। और अगर मनुष्य होने के नाते उससे कोई गुनाह हो ही जाएगा तो अनिवार्यतः उसे अपनी ग़लती का एहसास होगा और वह पछताएगा कि काश यह गुनाह उससे न हुआ होता! यह दुख और यह पछतावा इस बात का प्रमाण है कि उसमें ईमान की शक्ति मौजूद है। इसलिए अनिवार्यतः वह प्रायश्चित करेगा और क्षतिपूर्ति के प्रयास में लग जाएगा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से हम भली-भाँति समझ सकते हैं कि ईश्वर के रसूल सदैव कर्म पर उभारते हैं। उनकी शिक्षा यह है कि अपने ईमान और विश्वास का निरीक्षण करते समय हम अपने कर्मों और उनके प्रभावों पर नज़र डालें जो हमारे दिलों पर पड़ते हैं।
इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि गुनाह की प्रकृति ही यह है कि उससे हृदय को शान्ति नहीं मिलती। हृदय अगर मोमिन है तो गुनाह ही नहीं, उसे तो वह चीज़ भी खटकेगी जो गुनाह के सदृश होगी, या जो आदमी को गुनाह और बुराई से निकट कर सकती हो। इसलिए सावधानी इसी में है और सर्वश्रेष्ठ नीति यही है कि आदमी हर उस चीज़ से जो हृदय में मलिनता, दुविधा और खटक पैदा करनेवाली हो, परहेज़ करे। इस तरह इन्शाअल्लाह वह प्रत्येक प्रकार की बुराई और गुनाह से सुरक्षित रहेगा। इसकी पुष्टि इस हदीस से भी होती है—
‘‘उस चीज़ को छोड़ दे जो तुझे शक में डाले और उस चीज़ की ओर ध्यान दे जो तुझे किसी संशय में न डाले। इसलिए कि सच्चाई शान्ति है और झूठ सर्वथा संशय और दुविधा।” (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, नसई)
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सत्य की विशिष्टता ही यह है कि वह शान्ति का कारण होता है जबकि असत्य और झूठ पर चलनेवाला व्यक्ति कभी भी सन्देहों, उलझनों और भ्रान्तियों से अपने दामन को नहीं छुड़ा सकता। अच्छाई और बुराई के पहचानने का जो नियम आप ने बताया है उसमें यह बात भी दृष्टि में रहे कि यह नियम उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में ईश-भय का गुण विद्यमान हो।
दुख और चिन्ता
(1) हज़रत साद-बिन-अबी-वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि “यह क़ुरआन वेदना और पीड़ा के साथ अवतरित हुआ है। अतएव जब इसे पढ़ो तो रोओ, और अगर रोना न आए तो रोने की शक्ल बनाओ। और इसे अच्छी आवाज़ में पढ़ो। जिस व्यक्ति ने क़ुरआन को अच्छी आवाज़ में न पढ़ा वह हममें से नहीं।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : क़ुरआन की गहराइयों में उतरने के लिए आवश्यक है कि आदमी का हृदय दर्द और वेदना से परिचित हो। क़ुरआन हमारे अन्दर दर्द और वेदना के भाव जगाता है। सम्भवतः वेदना और व्यथा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अधिक विश्वसनीय और प्रभावकारी होता है। सत्य के पाने का लक्षण यह है कि आदमी की आँखों से अश्रुधाराएँ बह निकलें। बेताबी और अत्यधिक दुख की घड़ियों ही में नहीं, निकटतम सामीप्य और चरम आनन्द के क्षणों में भी हृदय के भावों की अभिव्यक्ति यदि सम्भव है तो आँसुओं और नम आँखों के द्वारा ही सम्भव है। क़ुरआन में है—
“जब वे उसे सुनते हैं जो रसूल पर अवतरित हुआ है, तो तुम देखते हो कि उनकी आँखें आँसुओं से छलकने लगती हैं, इसलिए कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया है।" (5:83)
एक दूसरी जगह कहा गया है—
“जब उन्हें रहमान की आयतें सुनाई जाती हैं तो वे सज्दे करते और रोते हुए गिर पड़ते हैं।" (19:58)
एक अन्य स्थान पर है—
"जिनको इसके पहले से ज्ञान प्राप्त है उन्हें जब यह पढ़कर सुनाया जाता है तो वे ठोढ़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि महान है हमारा रब! हमारे रब का वादा तो पूरा होकर ही रहता है और वे रोते हुए ठोढ़ियों के बल गिरते हैं, और यह (क़ुरआन) उनके विनय और भक्तिभाव को और बढ़ा देता है।" (17:107-109)
क़ुरआन मानवता को मुक्त करने और उसे सफल बनाने के लिए सत्य के प्रसार और सत्यधर्म की स्थापना का दायित्व अपने अनुयायियों पर डालता है। इस दायित्व का निर्वाह सही अर्थों में उस समय तक सम्भव नहीं जब तक कि हमारे हृदयों में मानवमात्र के लिए अगाध प्रेम न पाया जाता हो और हमें उनके दुखों और चिन्ताओं से सरोकार न हो। इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाह में हम तभी सफल हो सकते हैं जबकि हमारे हृदय ईश-भय से परिपूर्ण हों और ईश्वर के बन्दों की मुक्ति की चिन्ता ने दिल का चैन और आराम हमसे छीन लिया हो।
क़ुरआन-पाठ की विधि यह है कि क़ुरआन पढ़ते हुए हमारे हृदय पिघले हुए हों और हम इसके प्रभाववश रो रहे हों। क़ुरआन से पूर्णतया लाभान्वित होने के लिए मात्र गहन चिन्तन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ रोना भी आवश्यक है। रो न सके तो रोने की मुद्रा ही बना ले, क्योंकि यह चीज़ भी हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है।
आदमी को चाहिए कि क़ुरआन को अच्छी आवाज़ में पढ़े। दर्द के साथ और द्रवित स्वर में पाठ करे। यह क़ुरआन का एक बड़ा हक़ है। इससे ईश-वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। वह मृदुल से मृदुल हो जाती है। ईश-भय की अपेक्षा भी यही है कि क़ुरआन को दर्द की आवाज़ में पढ़ा जाए। इससे हुज़ूरी के भाव में प्रगति होती है। इससे हृदय की जड़ता और निष्ठुरता दूर होती है और वह अत्यन्त कोमल हो जाता है।
अच्छी आवाज़ से पढ़ने के लिए मूल में "य-त-ग़न्ना" शब्द आया है। कुछ विद्वानों ने इसका यह अर्थ लिया है कि क़ुरआन उसे लोगों से बेनियाज़ कर दे। क़ुरआन जैसी नेमत पाकर भी जिन लोगों के हृदय धनी न हो सकें वे सही अर्थों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के तरीक़े पर नहीं हैं। लेकिन इसे अच्छी आवाज़ से पढ़ने के अर्थ में लेने की पुष्टि कुछ दूसरी स्पष्ट हदीसों से होती है। उदाहरणार्थ, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है, “सुशोभित करो क़ुरआन को अपनी आवाज़ों से।” (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)
दूसरे अर्थ की पुष्टि में भी हदीसें मौजूद हैं।
(2) हज़रत अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का वर्णन है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना कि “मोमिन को जो तकलीफ़, कष्ट, रोग और दुख हो, यहाँ तक कि वह चिन्ता भी जो उसे होती है, अनिवार्यतः उससे उसकी बुराइयाँ और गुनाह मिट जाते हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मोमिन की कोई चीज़ भी अकारथ नहीं जाती। उसके महान चरित्र के साथ-साथ उसके सत्कर्म तो भलाई और प्रतिदान का कारण होते ही हैं, वह अपने जीवन में जिन विपत्तियों और बीमारियों से दोचार होता है, यहाँ तक कि वे ग़म और परेशानियाँ भी जो दुनिया में हरेक को पेश आती ही हैं, मोमिन को उसकी वैसी परेशानियों के कारण भी लाभ पहुँचता है। उनके कारण ईश्वर उसके हृदय से कितनी ही बुराइयों के प्रभाव मिटा देता है और उसके कितने ही गुनाहों को क्षमा कर देता है। यह विशिष्टता जो मोमिन को प्राप्त है कोई साधारण बात हरगिज़ नहीं है। इससे भली-भाँति अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ईश्वर मोमिनों के लिए कितना कृपाशील है और मोमिन पर उसकी इनायतें और रहमतें कितनी ज़्यादा हैं।
व्यर्थ चीज़ों का त्याग
(1) हज़रत अली-बिन-हुसैन से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी के इस्लाम का सौन्दर्य और उत्कृष्टता यह है कि वह उस चीज़ को छोड़ दे जो बेफ़ायदा हो।” (हदीस : मुवत्ता, मुस्नद अहमद)
व्याख्या : यह सहीह हदीस है। हदीस के ग्रंथों में यह हदीस विभिन्न रावियों से उल्लिखित है। इब्ने-माजा ने इसे अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से और तिर्मिज़ी, बैहक़ी और अहमद ने अली-बिन-हुसैन (हज़रत ज़ैनुल-आबिदीन) और अबु-हुरैरा दोनों के माध्यम से इसका उल्लेख किया है। हाकिम इसका अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के माध्यम से उल्लेख करते हैं।
मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में इस्लाम अपने सम्पूर्ण सौन्दर्य और सम्पूर्ण उत्कृष्टता के साथ सम्मिलित होगा वह इस्लाम की बरकतों से पूर्णतया लाभान्वित होगा। इस्लाम का सौन्दर्य उसके जीवन को भी सौन्दर्य और गुणों से परिपूर्ण कर देगा। उदाहरणार्थ ऐसा व्यक्ति, ऐसी बातों, ऐसे कामों और ऐसे विचारों से अपने को दूर रखेगा जिनका कुछ हासिल नहीं होता, जो न दुनिया के लिए लाभकारी हैं और न आख़िरत में उनसे कोई लाभ पहुँचने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाएगा जो नेकी के काम हैं और जिनसे ईश्वर की प्रसन्नता और उसकी रज़ामन्दी हासिल होती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने समय, अपनी ऊर्जा और धन को नष्ट होने से बचा सकता है। फिर इसके साथ उसे जो एकाग्रता, शान्ति और परितोष प्राप्त होगा, इसका अन्दाज़ा उन लोगों को नहीं हो सकता जिनकी ऊर्जा व्यर्थ कार्यों में नष्ट होती है, और वे व्यर्थ कार्य उनकी बौद्धिक व मानसिक उलझनों और हार्दिक विकेन्द्रता और व्यग्रता का कारण बनते हैं और उनके उजाड़ हृदय तृष्णा और सन्ताप के भयावह बसेरे बनकर रह जाते हैं।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि सहाबा में से एक व्यक्ति का निधन हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा कि तेरे लिए स्वर्ग की शुभ सूचना है! इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या कह रहा है, जबकि वस्तुस्थिति से तू अवगत नहीं। शायद उसने व्यर्थ वार्तालाप किया हो या ऐसे मामले में कृपणता दिखाई हो जिसमें उसके लिए कोई हानि न थी।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : एक व्यक्ति ने सहाबी को सम्बोधित करके कहा था कि तेरे लिए स्वर्ग की शुभ सूचना है। तू कितना भाग्यशाली है, स्वर्ग तेरी प्रतीक्षा में है! इसपर अल्लाह के रसूल ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे मालूम हुआ कि धर्म और नैतिकता का मामला कितना नाज़ुक है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई घोर अपराध न भी किया हो तब भी उसकी व्यर्थ और बेफ़ायदा बातचीत उसके स्वर्ग-प्रवेश में आड़े आ सकती है। अनर्गल और अशिष्ट वार्तालाप से भी आदमी की पोज़ीशन ख़राब हो सकती है और वह विपत्ति का शिकार हो सकता है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ किसी के स्वर्ग में जाने की घोषणा करना तक़वा के प्रतिकूल है।
यह हदीस यह भी बताती है कि आदमी ऐसी चीज़ों में कृपणता से काम लेकर अपनी निम्नता और अनुदारता का प्रमाण देता है जिसमें आदमी के लिए हानि की कोई बात नहीं होती। उदाहरणार्थ, सलाम करना, प्रसन्न मुद्रा में भाई का स्वागत करना, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, आदि। यह कृपणता आदमी और उसके स्वर्ग के बीच रोक बन सकती है।
क़ुरआन और हदीस से यह भी मालूम होता है कि सदक़े से भी आदमी के धन में कमी नहीं होती। सदक़ा और भलाई के दूसरे कामों में ईश्वर ने बरकतें ही रखी हैं। क़ुरआन में है—
“और तुम जो भी ख़र्च करोगे, वह उसकी जगह तुम्हें और देगा।" (34:39)
हदीस में है—
“सदक़े से माल में कमी नहीं आती।” (हदीस मुस्लिम)
“भलाई के कामों में ख़र्च करो, तुमपर ख़र्च किया जाएगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
(3) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने फ़र्श का ज़िक्र आया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “एक फ़र्श तो आदमी को अपने लिए दरकार है और एक फ़र्श पत्नी के लिए और एक फ़र्श मेहमान के लिए। अब चौथा शैतान के लिए होगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अनावश्यक साज़ो-सामान रखने का अर्थ यह है कि आदमी अपने समय और दौलत के एक बड़े हिस्से को वहाँ ख़र्च कर रहा है जहाँ ख़र्च करने की वास्तव में कोई आवश्यकता न थी। शैतान यही चाहता भी है कि वह आदमी को अस्ल कामों से हटाकर उसके धन और समय को दूसरे अनावश्यक कार्यों में ख़र्च कराए और उसे व्यर्थ की व्यस्तताओं में उलझाए रखे। आवश्यकता से अधिक सामान रखना दम्भ और अपव्यय है। इससे मोमिन को परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता यदि वास्तव में आवश्यकता है, उदाहरणार्थ, अतिथियों का बाहुल्य रहता है तो एक से अधिक बिस्तर रखने में कोई हर्ज नहीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का उद्देश्य वास्तव में उस मानसिकता का सुधार है जो साधारणतया सांसारिक लोगों की हुआ करती है।
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर ने हमें यह आदेश नहीं दिया है कि जो कुछ उसने हमें (धन आदि) दिया है, उसे हम पत्थरों और ईंटों पर कपड़े लटकाने में ख़र्च करें।" (हदीस : अबूदाऊद)
व्याख्या : यह एक लम्बी हदीस का अंश है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिहाद के किसी सफ़र पर थे। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की प्रतीक्षा में थीं। उन्होंने मकान पर एक कपड़ा सजाने के लिए लगा दिया था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लौटे तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दृष्टि उसपर पड़ी और आपके चेहरे से अप्रसन्नता ज़ाहिर हुई। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस कपड़े को उतार दिया और वह बात कही जो यहाँ उद्धृत की गई है।
इस हदीस का अर्थ यह है कि ईश्वर के दिए हुए धन का यह कोई उचित प्रयोग नहीं है कि उसे हम ईंट और पत्थर को कपड़े से सजाने में व्यय करें। जो रुपए हम इस काम में ख़र्च करेंगे, वे दूसरे नेक कामों में ख़र्च किए जा सकते हैं। इस्लाम में सादगी को इसी लिए पसन्द किया गया है। इसमें अपव्यय की सम्भावना नहीं रहती और यह बात हमेशा ध्यान में रहती है कि सुख-सुविधा, आनन्द और सौन्दर्य प्रदर्शन का वास्तविक स्थान यह नश्वर संसार नहीं बल्कि पारलौकिक जगत् है। उस शृंगार से क्या हासिल जो क्षणिक है। उस वसंत पर क्या मुग्ध हों और क्यों मुग्ध हों जो शीघ्र ही पतझड़ में बदल कर रहेगा।
प्रसिद्धि-कामना से परहेज़
(1) हज़रत साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"अल्लाह को वह बन्दा प्रिय है जो ईशपरायण, बेनियाज़ और गुमनाम हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर अपने ऐसे बन्दे को पसन्द करता है जिसके अन्दर ये तीन गुण मौजूद हों। प्रथम यह कि वह प्रत्येक मामले में ईश्वर से डरता और सत्य-असत्य का ध्यान रखता हो। दूसरा यह कि वह हृदय का धनी हो अर्थात उसमें आत्मसम्मान और सन्तोष का गुण पाया जाता हो। आत्मिक परितोष का धन उसे प्राप्त हो। अस्ल धन यही है। यूँ इस्लाम की दृष्टि में धन-दौलत भी बुरी चीज़ नहीं है, शर्त यह है कि आदमी परहेज़गार और ईश्वर का कृतज्ञ हो। तीसरा गुण जिसका ज़िक्र इस हदीस में किया गया है वह यह है कि आदमी गुमनामी को पसन्द करता हो। वह प्रसिद्धि का भूखा न हो। जो नेक कर्म भी करता हो, मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उसकी अभिलाषा होती है कि जो धन भी वह ईश्वरीय मार्ग में ख़र्च करता है या जिस नेक काम का उसे सुअवसर प्राप्त होता है उसकी ख़बर लोगों को न हो सके।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि "जो व्यक्ति अपने कर्म का लोगों में प्रचार करेगा अल्लाह उसकी इस रियाकारी और दिखावे से लोगों को अवगत करा देगा और उसे तुच्छ और क्षुद्र बना देगा।" (हदीस अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : अर्थात जो प्रसिद्धि और नामवरी का भूखा व्यक्ति यह चाहेगा कि लोगों के कानों तक यह बात पहुँच जाए कि उसने ये नेक काम किए हैं तो लोगों को उसके इस कर्म की सूचना तो हो जाएगी मगर साथ ही लोगों को इस बात की भी ख़बर हो जाएगी कि वह दिखावा करनेवाला, प्रसिद्धि का भूखा और एक गिरा हुआ आदमी है। उसके कर्म से लोग उसे नेक और सौभाग्यशाली समझने के बजाए एक तंगदिल और हीन व्यक्ति ही समझेंगे। इस प्रकार ईश्वर ऐसे लोगों को अपमानित करके रहता है। उन्हें सच्ची नामवरी और लोकप्रियता कभी भी प्राप्त नहीं होती।
आदर
(1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो हमारे छोटे पर दया न करे और हमारे बड़े का हक़ न पहचाने वह हममें से नहीं।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : "वह हममें से नहीं" अर्थात उसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं। वह हमारे तरीक़े पर नहीं है। छोटों का हक़ है कि उनके साथ मेहरबानी से पेश आया जाए। वे हमारे प्रेम और कृपादृष्टि के पात्र होते हैं। इसी प्रकार बड़ों का भी हमपर हक़ होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें। उनके साथ हमारा व्यवहार अशिष्टता का न हो। जहाँ तक सम्भव हो उनकी सेवा ही करें।
(2) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"वह व्यक्ति हममें से नहीं जो हमारे छोटे पर दया न करे और हमारे बड़े का आदर और सम्मान न करे।" (हदीसः तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस अर्थ की हदीसें विभिन्न हदीस-ग्रंथों, मुस्नद अहमद, हाकिम, तबरानी आदि में विभिन्न उल्लेखकर्ताओं के माध्यम से वर्णित हुई हैं।
मूल्यों का सम्मान
(1) हज़रत अबू-हूरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब तुममें से कोई किसी को क़त्ल की सज़ा दे तो उसके चेहरे को बचाए, इसलिए कि ईश्वर ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : न्याय का तक़ाज़ा हो तो आदमी को क़त्ल की सज़ा देनी पड़ सकती है। ऐसे अवसर पर भी आदेश है कि अपराधी के चेहरे का सम्मान किया जाए। न तो उसे बिगाड़ा जाए और न उसे क्षत-विक्षत किया जाए।
चेहरा आदमी के व्यक्तित्व और उसके सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक गुणों का दर्पण होता है। वास्तव में ईश्वर ने अपने गुणों की छाया मानव पर डाली है। इसलिए मानव एक रचना होने के बावजूद अपने रचियता और सृष्टिकर्ता के सौन्दर्य और प्रताप दोनों का प्रतीक है।
कुछ विद्वान कहते हैं कि 'अपनी सूरत पर' में जो सर्वनाम है वह ईश्वर के बजाय आदम के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आदम को आदम की सूरत पर पैदा किया। उसे सृष्ट प्राणियों में विशिष्टता प्रदान की। इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए लेकिन दूसरी हदीस से इस विचार का निषेध होता है। दारक़ुतनी में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जब तुममें से कोई मारे तो चेहरे को बचाए क्योंकि इन्सान का चेहरा रहमान की सूरत पर (रचा गया) है।" इन्सान में जीवन, ज्ञान, संकल्प और सामर्थ्य जैसे गुण पाए जाते हैं। वह देखता, सुनता और बोलता है। ये ईश्वर के भी गुण हैं। यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि इन्सान के गुण ईश्वरीय गुणों ही की छाया हैं।
मुखारबिन्दु और बाह्य सौन्दर्य जो इनसान को प्राप्त है वह वास्तव में अभौतिक और आत्मिक सौन्दर्य का प्रतीक है। इस दुनिया में आत्मिक सौन्दर्य का ज्ञान लौकिक प्रतीकों के बिना सम्भव नहीं है। लौकिक प्रतीकों के द्वारा ही उसका सम्बोध होता है। इसकी मिसाल रंग और प्रकाश की है। वास्तव में यह प्रकाश ही है जो रंगों के रूप में अभिव्यक्त होता है किन्तु यह प्रकाश रंगों में निहित होता है।
विशुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं होती, फिर भी हमें प्रकाश का अभिज्ञान रंग के माध्यम से हो जाता है।
(5)
गरिमा और महानता
उच्च साहस
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शक्तिशाली मोमिन अल्लाह की दृष्टि में दुर्बल मोमिन से अच्छा है और प्रत्येक में भलाई पाई जाती है। जो चीज़ तुम्हारे लिए लाभदायक हो उसके अभिलाषी बनो और ईश्वर से सहायता के इच्छुक हो और असमर्थ न हो, और अगर तुम्हें कोई संकट आ पड़े तो यह न कहो कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि यह कहो कि अल्लाह ने यही निश्चित किया था और उसने जो चाहा किया। क्योंकि यह 'यदि' शब्द शैतानी कर्म का द्वार खोलता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : शक्तिशाली मोमिन वह व्यक्ति है जिसे अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और विश्वास हो, जो भले कामों में आगे-आगे रहे, जो लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कार्यरत हो और इस सिलसिले में पेश आनेवाली कठिनाइयों और हतोत्साहित कर देनेवाली परिस्थितियों की परवाह न करते हुए उस महान कार्य को न छोड़े जिसे पूरा करने का प्रयास एक मोमिन का सबसे बड़ा दायित्व है।
इस हदीस से मालूम हुआ कि भलाइयों और गुणों से रिक्त तो कोई मोमिन हो ही नहीं सकता चाहे वह कमज़ोर इरादोंवाला मोमिन ही क्यों न हो। रहा वह व्यक्ति जिसके अन्दर सिरे से कोई भलाई पाई ही न जाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता।
जिस प्रकार हर क़िस्म की बुराइयों से बचना हमारे लिए आवश्यक है उसी प्रकार हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हमारे अन्दर ऐसी चीज़ों और ऐसे कार्यों की उत्कट इच्छा और अभिलाषा पाई जाए जो लौकिक और पारलौकिक जीवन में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हों। यह भी ज़रूरी है कि ईश्वर से सहायता और सहयोग की प्रार्थना की जाए। इसमें कभी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। काम सदैव ईश्वरीय सहायता और सहयोग ही से बनते हैं। ईश्वरीय अनुग्रह ही से बन्दे को इसकी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वह फ़ितने से भरी इस दुनिया में स्वयं को विभिन्न प्रकार की वैचारिक और व्यावहारिक गुमराहियों से बचा सके।
इस हदीस में यह जो कहा गया है कि 'अल्लाह ने यही निश्चित किया था और उसने जो चाहा किया', क़ुरआन से भी इसका समर्थन होता है। क़ुरआन में है—
“कह दो हमें कुछ भी पेश नहीं आ सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है। वही हमारा स्वामी है। और ईमानवालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।" (9:51)
एक दूसरी जगह पर कहा गया है—
“कह दो, यदि तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों का मारा जाना निश्चित था वे निकलकर अपने अन्तिम शयनस्थलों तक पहुँच कर रहते।" (3:154)
इससे ज्ञात हुआ कि जो कुछ बीत जाए उसपर दुख व क्षोभ में पड़कर अपना समय नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं। आदमी को चाहिए कि ईश्वर के फ़ैसले पर राज़ी रहते हुए अपनी शक्ति और सामर्थ्य भविष्य की चिन्ता में लगाए। शैतान तो चाहता ही है कि आदमी मुसीबतों में अपनी बेतदबीरी पर इलज़ाम लगाकर अपने आप को कोसे और अपने अतीत का मातम करता रहे। धैर्य व सहनशीलता को त्याग कर ईश्वर की पसन्द और उसकी इच्छा सभी कुछ भूल बैठे। अलबत्ता अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि आज्ञापालन में किसी कोताही पर अफ़सोस करने में कोई दोष नहीं। शर्त यह है कि आदमी अफ़सोस ही न करता रहे बल्कि अपनी कोताही को दूर करे और क्षतिपूर्ति करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करे। यह नहीं कि अपनी पिछली कोताही या गुनाह के ग़म ही में डूबा रहे। अपनी ग़लती या कोताही पर सिरे से किसी दुख का न होना तो ईमान के विरुद्ध है।
हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब नेकी करके तुझे ख़ुशी महसूस हो और बुराई करके पछतावा तो तू मोमिन है।"
अल्लमा सुयूती ने जामेअ् में एक रिवायत उद्धृत की है कि जिस व्यक्ति ने सांसारिक क्षति पहुँचने पर शोक किया वह नरक के निकट हो गया जबकि उसकी दूरी हज़ार बरस की है और जो पारलौकिक क्षति पर दुखी हुआ वह स्वर्ग (जन्नत) से निकट हो गया जबकि उसकी दूरी भी हज़ार बरस की है।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कौन मुझसे यह तलवार लेगा, और इसको वह व्यक्ति ले जो इसका हक़ अदा करे। उसे अबू-दुजाना ने ले लिया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह बात उहुद की जंग के दिन कही थी।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : उहुद की जंग के मौक़े पर दुश्मनों से सख़्त मुक़ाबला था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने घोषणा की कि कौन मुझसे यह तलवार लेता है। सभी लोगों के हाथ आपकी ओर बढ़े। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा इसे वही व्यक्ति ले जो इसका हक़ अदा कर सके। अर्थात जो वीरता के साथ दुश्मनों से लड़े और कदापि कमज़ोरी न दिखाए। वह तलवार हज़रत अबू-दुजाना ने ली और अत्यन्त वीरता का प्रदर्शन किया।
आत्मसम्मान
(1) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखत है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन को शोभा नहीं देता कि वह अपने आप को अपमानित करे।” लोगों ने पूछा कि वह अपने आप को कैसे अपमानित कर सकता है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ऐसी आज़माइश में स्वयं जा पड़े जिसकी सहनशक्ति उसमें न हो।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा, बैहक़ी)
व्याख्या : ऐसे कामों में हाथ डालना मोमिन के मर्यादानुकूल नहीं जिस के परिणामस्वरूप उसे अपमानित व लज्जित होना पड़े। सहाबियों को अपमान से अत्यन्त घृणा थी। इस्लाम ने आत्मसम्मान की शिक्षा देते हुए उन्हें अपमान व हीनभाव से सुरक्षित रहने का अतिरिक्त निर्देश दिया। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति अगर गणित में कुशल न हो तो उसे गणित से सम्बन्धित कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस चीज़ के योग्य हम नहीं हो सकते, अपने लिए उसकी ख़ुदा से दुआ करना भी उचित नहीं है।
अगर हम इस्लाम का गहराई से अध्ययन करें तो हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसरण ही से आत्मसम्मान की रक्षा सम्भव है। आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए बिना इस्लामी आदेशों का उल्लंघन और ईश्वर की अवज्ञा सम्भव नहीं।
धैर्य व शालीनता
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अशज्ज अब्दुल-क़ैस से कहा—
“तुममें दो स्वभावगुण ऐसे हैं जो अल्लाह को प्रिय हैं— धैर्य और शालीनता।" (हदीस : मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : बहरैन के क़बीले अब्दुल क़ैस का एक प्रतिनिधिमंडल 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल के पास आया था जिसके प्रमुख मुंज़िर-बिन-अयाज़ थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें 'अशज्ज' की उपाधि प्रदान की। प्रतिनिधिमंडल जब मदीना पहुँचा तो उसके सदस्य फ़ौरन ही नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिलने के लिए दौड़ पड़े लेकिन मुंज़िर ने ऐसा न किया। वे अत्यन्त शान्तिपूर्वक सवारी से उतरे, सामान आदि को ढंग से रखा। सवारियों को चारा पानी दिया और फिर स्नान किया, कपड़े बदले, मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और फिर अत्यन्त शालीनता से और आदर के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनका यह ढंग बेहद पसन्द आया और उनके सम्बन्ध में वह बात कही जिसका उल्लेख इस हदीस में है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को न तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनकी अधीरता पर टोका और न उन्हें बुरा कहा। अलबत्ता आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुंज़िर की प्रशंसा की।
अबू-दाऊद की एक रिवायत में यह भी है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से मुंज़िर ने अपनी प्रशंसा सुनी तो कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! इन गुणों का सम्बन्ध मेरे प्रयास से है या ईश्वर ने इन्हें मेरा स्वभाव बनाया है?" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ईश्वर ने इन्हें तेरा स्वभाव बनाया है।" इसपर मुंज़िर ने कहा कि प्रशंसा उस ईश्वर की जिसने मुझे इन दो गुणों के साथ पैदा किया जो ईश्वर और उसके रसूल को प्रिय हैं। अर्थात चूँकि ये स्वभावगुण नैसर्गिक हैं इसलिए उनके पतन की सम्भावना नहीं रहती।
(2) हज़रत साद-बिन-अबी वक्क़ास से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल) ने कहा—
“विलम्ब और ढील हर चीज़ में बेहतर है सिवाय पारलौकिक कर्म के।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : सांसारिक कार्यों के विषय में मनुष्य नहीं जानता कि उनके करने का परिणाम अच्छा होगा या बुरा। इसलिए उनमें सावधनी और सोच-विचार से काम लेना ज़्यादा उचित है। उनमें जल्दबाज़ी से काम न लें। वे कार्य जिन का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन (आख़िरत) से है उनके शुभ और लाभप्रद होने में कोई सन्देह नहीं होता और जिनके प्रशंसनीय होने के सम्बन्ध में क़ुरआन और हदीस में स्पष्ट विवरण मौजूद हैं। अतः उनमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मालूम नहीं आदमी को फिर इनका सुअवसर मिले या न मिले। क़ुरआन में भी है कि—
"अपने रब की क्षमा और उस जन्नत की ओर अग्रसर होने में एक-दूसरे से बाज़ी ले जाओ जिसका विस्तार आकाश और धरती के विस्तार जैसा है, जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों।" (57:21)
एक दूसरी जगह कहा गया—
“अतः भलाई के कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ़ लौटना है।" (5:48)
अगर ईश्वरीय मार्ग में ख़र्च करने की इच्छा हो तो विलम्ब न करे। सम्भव है शैतान दिल में आशंकाएँ उत्पन्न कर ख़र्च करने से रोक दे। “शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और अश्लील कर्मों पर उभारता है जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा का तुम्हें वचन देता है। अल्लाह बड़ी समाईवाला, सर्वज्ञ है।" (2 : 268)
सांसारिक मामलों में जल्दबाज़ी के कारण अकसर ऐसा होता है कि हम ग़लत क़दम उठा लेते हैं और तत्पश्चात अपने किए पर पछताते हैं। कोई भी काम हो, गम्भीरता से उसके प्रत्येक पहलू पर दृष्टि डालनी चाहिए और उसके परिणामों के विषय में सन्तुष्ट हो लेना चाहिए। इस सिलसिले में दूसरे लोगों से परामर्श भी आवश्यक है, और इसके लिए ऐसा तरीक़ा और कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए जो सर्वाधिक उपयुक्त और लाभप्रद हो।
ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य केवल भविष्य की सम्भावना को देखते हुए किसी मामले में अनावश्यक रूप से पहले जल्दबाज़ी में ऐसा क़दम उठा लेता है जो उसके लिए अत्यन्त संकट और पश्चाताप का कारण बन जाता है। जिस सम्भावना को देखते हुए उसने वह क़दम उठाया था, समय आने पर ज्ञात होता है कि परिस्थिति अब दूसरी है और वह सम्भावित चीज़ सिर्फ़ एक भ्रम या सपना सिद्ध होती है। समय से पहले किसी बड़ी मजबूरी के बिना क़दम उठाना स्वयं को गम्भीर ख़तरे में डालना है।
संकुचित व सतही दृष्टि, लोभ-लिप्सा और सही सोच का अभाव जल्दबाज़ी और उतावलेपन के मुख्य कारण हैं। उदार हृदय और उदार दृष्टि रखनेवाला व्यक्ति ही इस स्थिति में होता है कि वह ठहरकर किसी विषय पर गम्भीरता से विचार कर सके और वह नीति अपनाए जिसमें भलाई हो। भलाई चाहनेवाला व्यक्ति मात्र भलाई का मार्ग ही नहीं अपनाता बल्कि इस प्रकार वह ईश्वर से सम्बद्ध हो जाता है। भलाई का यह पहलू स्वयं भलाई से भी बढ़कर सुन्दर और आनन्ददायक है। ठीक इसी तरह बुराई का मार्ग अपना कर मनुष्य न केवल यह कि बुराई में लिप्त हो कर रह जाता है बल्कि ईश्वर से भी उसका सम्बन्ध शेष नहीं रहता। बुराई का यह पहलू स्वयं बुराई से भी अधिक दुखद होता है। हदीस में है—
“अल्लाह तआला कहता है कि 'मैं दो साझीदारों में तीसरा हूँ जब तक उनमें से कोई विश्वासघात नहीं करता। किन्तु जब कोई एक विश्वासघात करता है तो मैं उनके बीच से निकल जाता हूँ।" (हदीस : अबू-दाऊद)
उदारता
(1) हज़रत अबुल-अहवस जुशम्मी अपने पिता से उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं किसी व्यक्ति के पास से गुज़रूँ और वह न तो मेरे मिलने का हक़ अदा करे और न मेरा सत्कार करे और उसके बाद उसका गुज़र मेरे पास से हो तो (क्या) मैं उसका सत्कार करूँ या मैं उससे (उसकी अनुदारता का) बदला लूँ? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "नहीं, बल्कि तुम उसका सत्कार करो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : “मैं उसका सत्कार करूँ" के लिए मूल में ‘अक़रिया' शब्द आया है। हाकिम की पांडुलिपि में 'अ-अक़रिया' आया है (अर्थात क्या मैं उसकी मेहमानदारी करूँ) लेकिन बाद की पांडुलिपि में प्रश्नवाचक 'हमज़ा' नहीं मिलता। हज़रत अबुल-अहवस जुशम्मी के पिता ने प्रश्न यह किया कि क्या मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूँ जो उसने मेरे साथ किया। मैं भी मुख फेर लूँ और उसका सत्कार न करूँ? आप ने यह शिक्षा दी कि तुम्हें तो प्रत्येक स्थिति में उदारता अपनानी चाहिए। कोई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है तुम्हें उसकी कुछ अधिक परवाह न होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की तंगदिली और संकीर्णता से प्रभावित होकर तुम अपनी नैतिकता को कदापि आघात न पहुँचाओ।
इस्लामी शिक्षाओं पर विचार करने से मालूम होता है कि इस्लाम हर मामले में यही चाहता है कि हम उदारता से काम लें, अपनी विशाल-हृदयता और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दें और हरगिज़ किसी संकीर्णता से काम न लें, बल्कि पैग़म्बरों और उनके सच्चे अनुयायियों का अनुसरण करें जो हमेशा चरित्र व व्यक्तित्व की महानता और उच्चता पर क़ायम रहे और कभी एक क्षण के लिए भी पसन्द न किया कि उस उच्च स्थान से नीचे उतर आएँ जिसे ईश्वर ने अपनी विशेष अनुकम्पा से उन्हें प्रदान किया था।
(2) हज़रत अम्र-बिन-अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में पहुँचकर पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान क्या है? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “धैर्य और उदारता।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि ईमान को केवल धारणा और सिद्धान्त बन कर नहीं रहना चाहिए। ईमान तो वही है जो मनुष्य का चरित्र बन जाए। ईमान की एक मौलिक अपेक्षा यह है कि आदमी दुनिया में धैर्य और दृढ़ता को अपना स्वभाव बनाए। वह जानता हो कि ईश्वर सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। वह हमारी स्थिति से अनभिज्ञ कैसे रह सकता है और हमें विवश और असहाय कैसे छोड़ सकता है? इसलिए अगर कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़े तो वह धैर्य और साहस से काम ले और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए अत्यन्त सतर्कता से अपने दायित्व के निर्वाह में लगा रहे।
फिर एक मोमिन व्यक्ति यह भी जानता है कि इनसान की वास्तविक सफलता वह है जो उसे आख़िरत में प्राप्त होगी। किसी भी कार्य की अन्तिम परिणति आख़िरत ही में देखने को मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आख़िरत की प्रतीक्षा नहीं कर सकता और सब कुछ दुनिया ही में देख लेना चाहता है तो उसकी यह इच्छा ईश्वरीय योजना के अनुकूल नहीं, उसके विरुद्ध है। ईमान का मतलब ही यह होता है कि जीवन में हमारे समक्ष हमेशा ईश्वर की योजना और उसकी स्कीम हो। ईश्वरीय योजना दीर्घकालिक होती है जिसको दृष्टि में रखना उसी समय सम्भव है जबकि हममें धैर्य का गुण पूर्णतः पाया जाता हो।
उदारता के लिए मूल में 'समाहत' शब्द प्रयुक्त हुआ है। समाहत सर्वोच्च मानवीय गुणों में से एक है। यह एक ऐसी भावस्थिति है जिसके कारण मनुष्य उन सभी बातों से, चाहे उनका सम्बन्ध ज्ञान से हो या कर्म से, दूर रहता है, जिनको वह जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक समझता है। दूसरे शब्दों में समाहत यह है कि मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों का दास बनकर न रहे बल्कि वह उत्तम अभिरुचि एवं आस्वाद की रक्षा करे। उसमें नर्मी भी पाई जाती हो और विशाल-हृदयता भी। धन-सम्पत्ति के मामले में भी वह दानशील हो। अपनी कमाई में से निर्धनों और मुहताजों पर ख़र्च करना जानता हो। कामेच्छा के मामले में वह संयम और पवित्रता का ध्यान रखता हो। इस सम्बन्ध में हर प्रकार की पथभ्रष्टता उसके लिए असह्नीय हो। इसी प्रकार गुनाह के कामों में, चाहे दूसरों के लिए कितना ही आकर्षण क्यों न हो, वह ईश भय के कारण उनसे हमेशा बचता हो। संकट में वह धैर्य से काम लेता हो। सुख-चैन और ख़ुशहाली में ईश्वर का आभारी और उसके बन्दों पर मेहरबान हो।
(3) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे पर दया न करो।" सहाबियों ने कहा कि हममें से प्रत्येक दयाशील है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "मेरा आशय यह नहीं है कि तुममें से कोई अपने साथी पर दया करे बल्कि मेरा अभिप्राय सार्वजनिक दयालुता से है।" (हदीस : तबरानी)
व्याख्या : इस हदीस से यह स्पष्ट हुआ कि उसकी दया और कृपा सबके लिए हो। मात्र स्वजनों पर ही वह कृपालु न हो। समस्त मानवता उसकी दृष्टि में ईश्वर के कुटुम्ब के सदृश हो। जैसा कि एक हदीस में उसे यही स्थान दिया भी गया है।
वज़न
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन एक अत्यन्त हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आएगा लेकिन (ईश्वर के निकट) मच्छर के पंख के बराबर भी उसका वज़न न होगा। यह आयत पढ़ो— "हम क़ियामत के दिन उन के लिए कोई वज़न न रखेंगे।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में एक अत्यन्त मौलिक तथ्य का वर्णन हुआ है। भौतिकवादी दृष्टि में मनुष्य के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा की बात यह है कि वह देखने में सुखी-समृद्ध, स्वस्थ और बलवान हो किन्तु सत्य यह है कि प्रतिष्ठा और गरिमा का मानदण्ड कुछ और ही है। एक व्यक्ति देखने में बड़ी काया और क़द-काठीवाला हो सकता है। सम्भव है जनसाधारण उससे प्रभावित भी होते हों लेकिन यह चीज़ उसकी प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता और महानता के लिए पर्याप्त नहीं। एक व्यक्ति देखने में तो बड़े शारीरिक डील-डोल के साथ क़ियामत के दिन आएगा लेकिन ईश्वर की दृष्टि में उसका कोई महत्व न होगा। मच्छर के पंख के बराबर भी ईश्वर की दृष्टि में उसका वज़न न होगा, इसलिए कि ईश्वर के निकट प्रतिष्ठा का मानदण्ड नैतिकता और सदाचार है, न कि सांसारिक वैभव और शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति। यही कारण है कि सुशीलता और सत्कर्मों से रहित व्यक्ति आख़िरत में अपमानित होगा। ईश्वर के समक्ष तो मान-सम्मान के अधिकारी वही लोग होंगे जो वास्तव में इसके पात्र होंगे। जिनके जीवन में धन-सम्पत्ति और रूप-रंग का महत्त्व न था बल्कि जिन्होंने ईमान, नैतिकता और सदाचार को हमेशा अपने समक्ष रखा। संसार की कोई भी वस्तु जिनकी दृष्टि की उच्चता को पराजित न कर सकी। संसार की कोई दूसरी वस्तु ईमान और सदाचार के बदले में जिनके लिए आकर्षण का केन्द्रबिन्दु न बन सकी।
प्रतिष्ठा का मानदंड क्या है? इसे हम इस्लाम की स्पष्ट शिक्षाओं के प्रकाश में आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जिन्हें इस्लामी शिक्षाओं की कोई परवाह ही नहीं या जिनके दिलों में इस्लाम अभी उतरा ही नहीं उनका प्रतिष्ठा और गरिमा की वास्तविकता और उसके महत्व से परिचित होना अत्यन्त कठिन है। इसका परिणाम यह होता है कि सम्मान की खोज उन्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाती है लेकिन वे इससे वंचित ही रहते हैं। उस व्यक्ति की तरह जो हार्दिक परितोष और तृप्ति धन में ढूँढता है, लेकिन यह चीज़ उसके लिए सदैव दुर्लभ ही रहती है।
वास्तव में प्रतिष्ठा का मानदण्ड वह नहीं है जिसको ऐहिकवादियों ने प्रतिष्ठा का मानदण्ड समझ रखा है। एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने कभी अज्ञान को किसी के लिए प्रतिष्ठा का साधन नहीं बनाया और न कभी धैर्य और सहनशीलता के कारण किसी को अपमानित किया।"
एक और हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस व्यक्ति ने (अपने ऊपर होनेवाले) अत्याचार को क्षमा कर दिया, ईश्वर ने इससे उसकी प्रतिष्ठा में ही वृद्धि की।"
एक दूसरी हदीस है—
“जो आख़िरत की इज़्ज़त चाहता हो वह सांसारिक साज-सज्जा को त्याग दे।” अर्थात सांसारिक साज-सज्जा में ग्रस्त होकर न रह जाए, उसका अनुरागी न हो।
एक और हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन की श्रेष्ठता क़ियामुल्लैल (रात की इबादत) में है और प्रतिष्ठा लोगों से निरपेक्ष रहने में है।"
इन हदीसों से भली-भांति समझा जा सकता है कि प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता का वास्तविक सम्बन्ध मानव के व्यक्तिगत गुणों, परलोक प्रियता और ईश-भय से है, न कि किसी दूसरी चीज़ से।
क़ुरआन में है—
“वास्तव में अल्लाह के निकट तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार है।"
प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता वास्तव में ईश्वर की अमानत है। मानव का दायित्व है कि वह अपने आप को अपमान से बचाए। इस सिलसिले में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है—
“आदमी जिस चीज़ के द्वारा अपनी मर्यादा की रक्षा करे अल्लाह उसे उसके लिए सद्क़ा लिखेगा।"
मान-अपमान का वास्तविक मानदण्ड जान लेने के बाद यह बात सरलतापूर्वक समझ में आ जाती है कि इनसान स्वयं अपने मान-अपमान का ज़िम्मेदार है। आदमी अपने जीवन में जो भी नीति अपनाता है उसके परिणामस्वरूप या तो वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या वह अपने को पस्ती की ओर ले जाकर स्वयं को अपमानित करता है। दुनिया में मोमिन की अन्तर्दृष्टि से पूर्णतः इसका आभास हो जाता है कि प्रतिष्ठित कौन है और अपमानित कौन?
परलोक में चूँकि तथ्यों का उद्घाटन होगा इसलिए वहाँ यह सब ही पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने नफ़े का सौदा किया और किसने घाटा उठाया। आदमी दुनिया में चाहे किसी के साथ कोई मामला करता है लेकिन वास्तव में वह स्वयं अपने साथ मामला कर रहा होता है। इसलिए कि उसके प्रत्येक विचार और कर्म से उसकी हैसियत का निर्धारण होता है। जब वस्तुस्थिति यह है तो यह समझना कुछ कठिन नहीं रहता कि हमें अपना जीवन कितना सतर्क होकर व्यतीत करना चाहिए।
हदीस के अन्त में क़ुरआन की एक आयत भी उद्धृत की गई है कि क़ियामत के दिन ईश्वर के अवज्ञाकारियों के लिए कोई वज़न क़ायम न होगा। उस दिन वे बेवज़न होंगे। उनके हिस्से में निन्दा और अपमान के सिवा कोई दूसरी चीज़ न आएगी। जो चीज़ उन्हें उस दिन वज़नदार बना सकती थी वह चरित्र और नैतिकता का वज़न था जिससे बेख़बर होकर वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुनिया में भी वे बेवज़न और मुर्दा थे, आख़िरत में भी वे बेवज़न ठहरेंगे। ऐसे लोगों का महत्व मलबे से कुछ अधिक नहीं होता। क़ुरआन में इस सत्य को विभिन्न स्थानों पर स्पष्ट किया गया है। मिसाल के तौर पर एक जगह कहा गया है—
“फिर जिस किसी के वज़न भारी होंगे, वह मनभाते जीवन में रहेगा। और रहा वह व्यक्ति जिसके वज़न हल्के होंगे, उसकी माँ होगी गहरा खड्ड। और तुझे क्या मालूम कि वह क्या है? आग है दहकती हुई।" (101:6-11)
इस हदीस में हमारे लिए बड़ी शिक्षा है। हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे दीन और ईमान ने चरित्र, विचार और नैतिकता की दृष्टि से हमें कितना वज़न प्रदान किया है। अगर हम प्रत्यक्ष धार्मिक कार्यों और रस्मों का पालन करने के बावजूद अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से कुछ भी ऊँचे न उठ सके बल्कि अधमता ही में पड़े रहे, विशाल हृदय होने के बजाए क्षुद्र ही बने रहे, तो इससे कुछ होने का नहीं है। ऐसी हालत में हम अपनी नमाज़ों और तस्बीहों का हिसाब करते रहें, इससे क्या अन्तर पड़ेगा। इससे वास्तविकता नहीं बदल सकती। हिसाब तो हमें अपने आप का करना चाहिए।
गरिमा और गम्भीरता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे बयान करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब नमाज़ की इक़ामत कही जाए तो तुम उसकी तरफ़ भगदड़ मचाते हुए मत आओ, बल्कि तुम शान्तिपूर्वक आओ। फिर जितनी नमाज़ तुम्हें मिल जाए अदा कर लो और जो न पाओ उसे पूरी कर लो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात नमाज़ के लिए इस प्रकार आओ कि गम्भीरता और शालीनता प्रकट हो। रक्अतें छूटने के डर से भाग-दौड़ मत करो। जो रक्अतें मिल जाएँ पढ़ लो, बाक़ी इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरी कर लो। भगदड़ मचाना नमाज़ की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है और यह चीज़ स्वयं मोमिन की गरिमा के भी विरुद्ध है।
यह बात ध्यान रखने की है कि उपासना और आज्ञापालन का आधार शान्ति और धैर्य है। उपासना के वास्तविक लक्ष्य अर्थात प्रभु-पुज्य के समक्ष अपनी उपस्थिति के आभास के लिए जो चीज़ अपेक्षित है वह है गम्भीरता और ईश-ध्यान, न कि अनियन्त्रित व्यवहार।
क़ुरआन में यह जो आया है कि “ऐ ईमान लानेवालो, जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ पड़ो और क्रय-विक्रय छोड़ दो।" (62:9)
तो इसका मतलब वास्तव में यह है कि जब नमाज़ के लिए बुलाया जाए तो ग़ाफ़िल न रहो बल्कि सारे काम छोड़कर नमाज़ के लिए चल पड़ो।
कारोबार में स्वयं को इस तरह न लगाओ कि नमाज़ की अनिवार्यता और ईश्वर के स्मरण से वंचित हो जाओ। मोमिन का जीवन न तो भौतिकवादी होता है, और न वह संन्यासी होता है। उसके जीवन में सन्तुलन पाया जाता है। वह न तो संसार को त्यागता है और न ईश्वर से विरक्त होता है। इस दशा में कि सांसारिक कार्यों में वह व्यस्त होता है लेकिन अज़ान की अवाज़ सुनते ही सब कामों को छोड़कर नमाज़ के लिए मस्जिद की ओर चल पड़ता है। और नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ जाने में वह कोई अनिच्छा और नीरसता नहीं दर्शाता। मस्जिद की ओर उसके क़दम उठते हैं तो पूरे शौक़ और उल्लास के साथ उठते हैं।
एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुममें से जब कोई व्यक्ति नमाज़ का इरादा करता है तो वह उसी समय से नमाज़ में प्रवेश कर जाता है।" (हदीस : मुस्लिम)
अर्थात नमाज़ का इरादा करते ही वह एक प्रकार से नमाज़ की दशा में हो गया। इसलिए उसे यथासम्भव नमाज़ की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। शान्ति, गम्भीरता और शालीनता नमाज़ की मर्यादाओं में शामिल हैं।
(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़बीला अब्दुल-क़ैस के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अशज्ज से कहा—
"तुम्हारे अन्दर दो ऐसे स्वभाव-गुण पाए जाते हैं जो अल्लाह को पसन्द हैं, और वे हैं धैर्य और शालीनता व सहनशीलता।" (हदीस : मुसलिम)
उल्लेखों से मालूम होता है कि जब क़बीला अब्दुल-क़ैस के प्रतिनिधिमंडल के लोग मदीना पहुँचे तो वे पहुँचते ही नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिलने के लिए दौड़ पड़े लेकिन अशज्ज ने जल्दबाज़ी से काम नहीं लिया। वे शान्तिपूर्वक सवारी से उतरे, सामान को ढंग से रखा, ऊँटों को चारा-पानी दिया, फिर स्नान करके शालीनता और शान्ति के साथ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनका यह तरीक़ा बहुत पसन्द आया और उन्हें सम्बोधित करके वह बात कही जो इस हदीस में वर्णित है।
शालीनता और शिष्टता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारी तरह ऐसी तेज़ी के साथ बात नहीं करते थे कि शब्द परस्पर अत्यन्त मिले हुए और संयुक्त हों। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस प्रकार बात करते थे कि अगर कोई गिननेवाला गिनना चाहता तो वह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वाक्य गिन सकता था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : तिर्मिज़ी की रिवायत में ये शब्द आए हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस प्रकार बात करते थे कि वाक्यों के बीच अन्तराल होता था (अर्थात वाक्य अलग-अलग होते थे) कि जो व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास बैठता था वह उसे याद रख सकता था।
किसी व्यक्ति की बातचीत और वार्तालाप से भी इस बात का पता चलता है कि वह आदमी कैसा है। शिष्ट और शालीन व्यक्ति की बातचीत भी गरिमापूर्ण होती है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बातों से आपकी शालीनता और शिष्टता प्रकट होती थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कदापि इस प्रकार बात नहीं करते थे जिसमें कहीं ठहराव न हो और न आपकी वाणी में वैसा अनुचित प्रवाह और तीव्रता होती थी कि शब्द और वाक्य परस्पर ऐसे मिल जाएँ कि सुननेवाले को सुनने और समझने में कठिनाई हो। सुननेवाला अगर चाहता तो वह सरलतापूर्वक आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बातों को याद रख सकता था, बल्कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शब्द और वाक्य तक गिने जा सकते थे।
दायित्वपूर्ण बात चीत की यही शान होती है। जो बात वास्तविक चेतना और सद्भाव से की जाएगी उसमें किसी प्रकार की असुन्दरता उत्पन्न नहीं हो सकती और सुननेवाले के लिए उसमें किसी संशय की गुंजाइश न होगी। फिर यह भी एक तथ्य है कि उलझी हुई बातचीत या अभिभाषण उलझे हुए मन-मस्तिष्क का परिचायक होता है। अगर मन में कोई तनाव और वैचारिक उलझाव है तो बातचीत या भाषण में भी इसका प्रभाव प्रकट होगा। सुनने वाले को कभी भी उससे पूर्ण सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-सरजस से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छा तौर-तरीक़ा, शालीनता और मध्यमार्ग नुबूवत का चौबीसवाँ अंश है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात ये गुण नुबूवत की विशिष्टताओं में से हैं। नबी मानवता के लिए पूर्ण आदर्श होते हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे उस का सम्बन्ध समाज से हो या राजनीतिक व आर्थिक जीवन से, वही तरीक़ा अपनाते हैं जो न्यायपूर्ण, यथार्थपरक, सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा और सम्पूर्ण तत्वदर्शिता के लिए अपेक्षित है। वे कभी भी शालीनता और शिष्टता के प्रतिकूल कोई नीति नहीं अपनाते। उनके यहाँ किसी प्रकार का अतिवाद नहीं पाया जाता। वे उस मार्ग को अपनाते हैं और उसी पर चलने का आह्वान करते हैं जो जीवन का स्वाभाविक और सीधा मार्ग है, जिसको अपनाकर मानव कठिनाइयों में नहीं पड़ता बल्कि जिसपर चलने से कठिनाइयाँ सुगम हो जाती हैं। नबी तो उन समस्त अज्ञानपूर्ण बन्धनों को खोलते हैं जिनमें मानवता जकड़ी हुई होती है। और वे उन समस्त अनुचित और अप्रिय बोझों को उतार फेंकने के लिए दुनिया में आते हैं जिनके तले दबकर मानवता कराह रही होती है। अतएव क़ुरआन में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—
‘‘और जो उन्हें भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, उनके लिए अच्छी-स्वच्छ चीज़ों को हलाल और बुरी अस्वच्छ चीज़ों को हराम ठहराता है और उनपर से उनके वे बोझ उतारता है जो अब तक उनपर लदे हुए थे और उन बन्धनों को खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे।" (7:157)
नबियों के प्रिय स्वभावों और गुणों को ही अपनाने में हमारी कामयाबी है। ईश्वरीय अनुकम्पा को अपनी ओर आकृष्ट करने का दूसरा कोई तरीक़ा सम्भव नहीं। जीवन में सम्यक् आचरण अपनाने पर व्यक्ति का सम्बन्ध मौलिक और अन्तिम सत्य (Ultimate Reality) से स्थापित हो जाता है जो मानव की सफलता की वास्तविक ज़मानत है। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी सत्य से सम्बन्ध स्थापित हो सकता है यद्यपि यथार्थ कोई भौतिक और सीमित वस्तु नहीं है। नुबूवत वह वास्तविक साधन है जिसके द्वारा इस भौतिक जगत् का सम्पर्क उस संसार से सथापित होता है। जो यथार्थ है और भौतिक सीमाओं से बँधा हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि सच्चे स्वप्न की कोई भौतिक व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका सम्बन्ध भी परोक्ष से होता है। यही कारण है कि हदीसों में सच्चे स्वप्न को नुबूवत का छियालीसवाँ अंश कहा गया है, इसलिए कि उनमें भी नुबूवत के प्रकाश की थोड़ी सी झलक हम देख लेते हैं।
सन्तुलन और मध्यमार्ग
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दीन आसान है। और दीन के सम्बन्ध में जो कोई कठिन नीति अपनाता है अनिवार्यतः दीन उसपर प्रभुत्त्व प्राप्त कर लेता है। अतः विशुद्ध सन्तुलन का मार्ग अपनाओ, प्रसन्न रहो और प्रातः व संध्या और रात्रि के कुछ अंश के द्वारा (ईश्वरीय आज्ञापालन में) सहायता चाहो।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इस्लाम एक स्वाभाविक धर्म है। इसमें कठिनाई और अनुचित परिश्रम अपने आप में अभीष्ट नहीं है। धर्म को हम उसी स्थिति में स्वाभावानुकूल धर्म कह सकते हैं जबकि वह हमारे लिए कोई मुसीबत न हो बल्कि उससे हमारी आत्माएँ चैन पाएँ और वह हमें अनुचित बन्धनों और कठिनाइयों से मुक्त करे।
जो व्यक्ति धर्म को स्वाभाविक रूप से अपनाने के बजाए धार्मिक मामलों में अतिवाद का रवैया अपनाता है वह अन्ततः पराजित होकर रहता है। धार्मिक आदेशों के पालन और उनपर सुदृढ़ रहने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म में मूल्य सत्य पर जमे रहने का है, सामयिक उत्साह और आवेश का कोई विशेष महत्व नहीं।
इस्लाम का स्वभाव यह है कि उचित और ठीक तरीक़ा अपनाओ। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मुताबिक़ कार्य करो। इसके विपरीत कोई नीति अपनाओगे तो धर्म तुम्हारे लिए कोई आनन्ददायक वस्तु न रहेगा। सत्य धर्म से परिचित कराकर ईश्वर तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता है। तुम्हें दुखी और परेशान देखना कदापि उसकी इच्छा नहीं है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मारे गए गहनता में पड़नेवाले अतिवादी!" (हदीस : मुसलिम)
तुम्हें चाहिए कि आनन्द और हार्दिक प्रसन्नता की घड़ियों में नेक काम और इबादत के द्वारा ईश्वर के आज्ञापालन के विषय में सहायता चाहो। वे घड़ियाँ हैं प्रातः, संध्या और रात्रि का अन्तिम पहर। हृदय को प्रसन्नता और निश्चिन्तता अगर प्राप्त नहीं तो इबादत और क़ियाम, रुकू और सज्दों में आनन्द नहीं मिल सकता। एक समझदार मुसाफ़िर अनुकूल समय में अपना मार्ग तय करता है और दूसरे समय में अपने लिए और अपनी सवारी के लिए आराम का अवसर जुटाता है। इस प्रकार वह बिना किसी थकावट और कठिनाई के अपनी मंज़िल पर पहुँच जाता है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने दिलों को समय-समय पर आराम पहुँचाओ।” (हदीस : अबू-दाऊद)
(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सदाचार और आन्तरिक एवं बाह्य शिष्टता और मध्यमार्ग नुबूवत का पच्चीसवाँ अंश हैं।
व्याख्या : मूल में आन्तरिक और बाह्य के लिए 'सम्तस्सालेह' शब्द प्रयुक्त हुआ है। सम्तस्सालेह से अभिप्राय है व्यक्ति के आन्तरिक और बाह्य आचरण और कर्म की विशुद्धता।
क़ुरआन और हदीसों में मध्यमार्ग और सन्तुलन पर बहुत ज़ोर दिया गया है। उदाहरणार्थ क़ुरआन में है—
“और अपना हाथ न तो अपनी गर्दन से बाँधे रखो, न उसे बिलकुल खुला छोड़ो।" (बनी-इसरईल सूरा-17)
अर्थात ख़र्च के मामले में सन्तुलन से काम लो।
एक दूसरी जगह कहा गया है—
“और जो ख़र्च करते हैं तो न तो अपव्यय करते हैं और न ही तंगी से काम लेते हैं, बल्कि वे इनके बीच मध्यमार्ग पर रहते हैं। (25:67)
एक और स्थान पर कहा गया है—
"ऐ आदम की सन्तान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपनी शोभा धारण करो; खाओ और पियो, परन्तु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़नेवालों को पसन्द नहीं करता।" (7:31)
प्रत्येक मामले में सही नीति मध्यमार्ग ही की होती है। अतिवाद, सख़्ती और अतिशयोक्ति किसी भी प्रकार उचित नहीं, बल्कि वह स्वयं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुसीबत ही मुसीबत है। इसी बात को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस प्रकार कहा है—
“अच्छी चीज़ें मध्यमार्गिक होती हैं।" (हदीस : बैहक़ी)
सम्ते-हसन और मध्यमार्ग साधारण चीज़ें नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को अपनाया, उसने वास्तव में नुबूवत के तरीक़े का अनुसरण किया। नुबूवत अपने भाव और वास्तविकता की दृष्टि से इतनी उच्च वस्तु है कि उसकी व्याख्या सम्भव नहीं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन गुणों का सम्बन्ध, जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है, नुबूवत से है। इसलिए कि नुबूवत भाव भी है और उच्चतम सुशीलता भी।
ख़ामोशी और मितभाषिता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या फिर ख़ामोश रहे। और जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। और जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने अतिथि का सत्कार करे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता और आख़िरत में सफलता के लिए आवश्यक है कि वह उन निर्देशों पर कार्यरत हो जो इस हदीस में दिए गए हैं। जो निर्देश दिए गए हैं वे सदाचार से सम्बन्धित हैं। इससे मालूम हुआ कि आख़िरत में हमारे लिए अच्छा घर जिस वजह से तैयार किया जाएगा वह सदाचार के सिवा कुछ और नहीं।
ईश्वर जिस चीज़ से प्रसन्न होता है वह वास्तव में आचरण की शुद्धता ही है लेकिन यहाँ यह बात हमारे सामने रहे कि इस्लाम में आचार-व्यवहार की कोई सीमित अवधारणा नहीं है बल्कि उसने दुनिया के सामने नैतिकता की अत्यन्त व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की है।
अनावश्यक बातें करना पसन्दीदा नहीं। बात उसी समय की जाए जब आवश्यक हो। बातों के साथ कितनी ही आपदाएँ लगी होती हैं जिनका आदमी को अन्दाज़ा भी नहीं होता। ऐसी बातें जिनमें न सवाब हो, न यातना, उनकी तुलना में भी ख़ामोशी को प्राथमिकता प्राप्त है। बात चीत में मालूम नहीं आदमी कब सीमाओं से आगे बढ़ जाए। फ़ुज़ैल-बिन-अयाज़ ने कहा है कि जो व्यक्ति बात को भी एक कर्म समझेगा वह निरर्थक बात कम करेगा। क़ुरआन में है—
“कोई बात उसने कही नहीं कि उसके पास एक निरीक्षक तैयार रहता है।" (50:18)
इसलिए आदमी को इस मामले में बेपरवाही से काम नहीं लेना चाहिए।
एक हदीस में ऊपर की हदीस के उस वाक्य के बजाए, जिसमें पड़ोसी का उल्लेख हुआ है, यह वाक्य आया है—
“जो व्यक्ति अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि वह नाते-रिश्ते को जोड़े रखे।"
इमाम इब्ने-ज़ैद मालिकी ने कहा है कि समस्त आचार-व्यवहार और सदाचार चार हदीसों से निकलते हैं, एक हदीस तो यही है। दूसरी हदीस है जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"आदमी के इस्लाम के सौन्दर्य में से यह है कि वह उस चीज़ को छोड़ दे जो उसके लिए निरर्थक हो।” (हदीस : मालिक, अहमद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी, बैहक़ी)
तीसरी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ग़ुस्सा न कर।" (हदीस : बुख़ारी)
चौथी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुममें से कोई मोमिन नहीं होता जब तक कि वह अपने भाई के लिए या यह कहा कि अपने पड़ोसी के लिए वही कुछ पसन्द न करे जो वह स्वयं अपने लिए पसन्द करता है।" (हदीस : मुस्लिम)
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस ने मौन धारण किया उसने मुक्ति पाई।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी, बैहक़ी)
व्याख्या : ख़ामोशी से कितनी ही भलाइयाँ जुड़ी हुई हैं और इसके द्वारा आदमी कितनी ही आपदाओं और बुराइयों से सुरक्षित रहता है। एक हदीस से मालूम होता है कि आदमी दोज़ख़ में ज़्यादातर ज़बान के बेलगाम होने के कारण औंधे मुँह गिराए जाते हैं। यह हदीस अत्यन्त संग्राहक है। शब्दों की दृष्टि से यह हदीस अत्यन्त संक्षिप्त है किन्तु इसके अर्थों में बड़ी व्यापकता पाई जाती है। इस हदीस में ख़ामोशी के लिए अरबी में सुकूत (चुप्पी) के स्थान पर 'सम्त' का शब्द आया है। जो अत्यन्त मार्मिक है। सम्त का अर्थ यह है कि आदमी बोलने की सामर्थ्य रखते हुए ख़ामोश रहे।
(3) हज़रत अनस से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ऐ अबू-ज़र! क्या मैं तुम्हें दो ऐसे स्वभाव-गुण न बताऊँ जो बहुत ही हल्के हैं पीठ पर और बहुत ही भारी हैं तुला में?" उन्होंने कहा, “क्यों नहीं, आप अवश्य बताएँ।” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अधिक ख़ामोशी और सुशीलता। उस सत्ता की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, लोगों ने इनके सदृश कोई कर्म नहीं किया।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ्बिल ईमान)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जिन दो प्रिय स्वभाव-गुणों का उल्लेख किया वे कितने आसान हैं। वे किसी के लिए कोई भारी बोझ नहीं किन्तु अपने महत्व और मूल्य की दृष्टि से अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। वे स्वयं तो हल्के और सहज हैं लेकिन अपने धारण करनेवाले को अत्यन्त बावज़न बना देते हैं।
एक गुण है ज़्यादा ख़ामोश रहने की आदत। जो व्यक्ति भी अनावश्यक ज़बान नहीं खोलेगा, अनुचित और अप्रिय बातों से बचेगा, अनिवार्यतः वह अधिक ख़ामोश रहेगा, बोलेगा कम। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में सहाबियों ने कहा है कि "अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ज़्यादा ख़ामोश रहते थे। आप वही बात करते थे जिसमें आपको अज्र व सवाब की उम्मीद होती थी।"
यह हदीस इसका स्पष्ट प्रमाण है कि लोगों के कर्मों में ये दोनों चीज़ें अर्थात ख़ामोशी और सुशीलता अप्रतिम हैं। कोई कर्म इन दोनों कर्मों से उच्च कोटि का नहीं।
(4) हज़रत अबू-ख़ल्लाद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब तुम किसी बन्दे को देखो कि उसे संसार से विरक्ति और मितभाषिता प्राप्त है तो उसका सामीप्य ग्रहण करो क्योंकि उसपर तत्वज्ञान प्रकाशित होता है।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ्बिल ईमान)
व्याख्या : अर्थात उसे सत्य-सम्बोध होता है। ईश्वर की ओर से उसके दिल में तत्वज्ञान डाला जाता है। उसकी वाणी सत्य की परिचायक बन जाती है। उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे इस बात का पता देते हैं कि उसपर ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। ईश्वर ने उसे भटकने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि वह उसका मार्गदर्शन करता रहता है। उसके मुख से जो कुछ निकलता है सत्य और लाभप्रद होता है। ऐसे व्यक्ति की संगति प्रभावकारी होती है। उसकी वाणी ही नहीं, उसकी मौनावस्था और उसकी दृष्टि में भी जादू का-सा असर होता है जिससे कितने ही जीवन बदल सकते हैं।
(5) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है कि—
"बुरे साथी से अकेले रहना अच्छा है। और नेक साथी अकेला रहने से अच्छा है। और भलाई की बातें सिखाना चुप रहने से अच्छा है और चुप रहना बुरी बातें सिखाने से अच्छा है।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : आदमी अपने संगी-साथियों के प्रभाव में होता है। साथी अगर अच्छे हैं तो आदमी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अगर साथी बुरे हैं तो वह उनके बुरे प्रभावों को ग्रहण करेगा। अच्छे साथी का विकल्प बुरे साथी नहीं हो सकते। इसलिए अगर अच्छे साथी न मिलें तो बुरे लोगों की संगति से अच्छा यह होगा कि आदमी उनसे अपने को दूर ही रखे। लेकिन अच्छे लोगों के रहते हुए एकान्त में रहना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार वह अच्छे लोगों से लाभान्वित न हो सकेगा। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि वे लोग जो ईमान और चरित्र की दृष्टि से इतने मज़बूत और पक्के हो चुके हैं कि बुरे लोगों की बुराइयों का प्रभाव ग्रहण नहीं कर सकते। वे अगर बुरों की इस्लाह के उद्देश्य से उनसे सम्पर्क और सम्बन्ध रखते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं बल्कि ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि वे उनसे सम्पर्क रखें ताकि अपने व्यक्तिगत प्रभावों और प्रयासों के द्वारा भटके हुए लोगों को राह पर ला सकें।
भलाई के प्रसार के महत्व से किसी को इनकार नहीं हो सकता। इसलिए वह व्यक्ति जो लोगों को भलाई से परिचित कराने के उद्देश्य से बात करता है वह उस व्यक्ति से अच्छा है जो चुप रहता है। अलबत्ता उस वार्तालाप से जो बुरे उद्देश्यों के लिए हो, चुप रहना ही बेहतर है। मालूम हुआ कि चुप रहना या बात करना स्वयं अभीष्ट नहीं है बल्कि हमारी बात चीत उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और हमारी ख़ामोशी भी अर्थ रखती हो।
(6) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। फिर उन्होंने विस्तृत हदीस बयान की। यहाँ तक कि अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि मैंने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे नसीहत कीजिए। आपने कहा— "मैं तुम्हें अल्लाह का डर रखने की नसीहत करता हूँ क्योंकि यह चीज़ तुम्हारे समस्त कर्मों को सबसे अधिक सुसज्जित करनेवाली सिद्ध होगी।” मैंने कहा कि कुछ और भी नसीहत करें। आपने कहा, "तुमपर क़ुरआन का पाठ और प्रतापवान ईश्वर का स्मरण अनिवार्य है क्योंकि यह आकाश में तुम्हारी चर्चा का कारण बनेगा और धरती में तुम्हारे लिए प्रकाश बनेगा। मैंने कहा कि कुछ और कहें। कहा, "तुमपर अधिक ख़ामोश रहना अनिवार्य है इसलिए कि यह चीज़ शैतान को दूर करनेवाली है और तुम्हारे दीनी कार्य में तुम्हारी सहायक है।" मैंने कहा कि कुछ और कहें। कहा, "ज़्यादा हँसने से बचो क्योंकि ज़्यादा हँसने से दिल मुर्दा हो जाता है और इससे चेहरा तेज रहित हो जाता है। मैंने कहा, "कुछ और भी कहें।" कहा कि "सच्ची बात कहो यद्यपि वह कड़वी हो।" मैंने कहा, "कुछ और भी कहें।" कहा कि “अल्लाह के मामले में किसी धिक्कारनेवाले की धिक्कार से न डरो।” मैंने निवेदन किया कि मेरे लिए कुछ और भी कहें। कहा, "जो कुछ तुम अपने विषय में जानते हो वह तुम्हें लोगों में दोष निकालने से रोक दे।” (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नसीहतों से मालूम हुआ कि हमारे समस्त कार्य की शुद्धता ईशभय पर निर्भर करती है। दुनिया और आख़िरत के सभी मामलों की शुद्धता की कुंजी ईशभय ही है। ईशभय के अभाव में सारे ही काम बिगड़ जाते हैं। लोग अगर ईशभय को अपने जीवन में उतार लें तो उनके आपसी मामलों में भी किसी प्रकार की कोई ख़राबी पैदा न हो और लोगों के सारे झगड़ों और शिकायतों का निपटारा हो जाए।
क़ुरआन की तिलावत और अल्लाह के स्मरण के द्वारा आदमी का सम्बन्ध उच्च लोक और सत्य की दुनिया से स्थापित हो जाता है। इस प्रकार धरती पर रहकर भी वह उच्च लोक का वासी हो जाता है। वह उसमें ख्याति प्राप्त कर लेता है और सांसारिक जीवन में यह चीज़ उसके लिए प्रकाश सिद्ध होती है। उसका जीवन प्रकाशमान हो उठता है। जीवन में कुछ भी असुन्दर और अशुभ शेष नहीं रहता। जीवन का सही मार्ग क्या है मानव जान लेता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन से ख़ामोशी के महात्म का ज्ञान होता है। इसमें सन्देह नहीं कि कितनी ही धार्मिक और सांसारिक आपदाओं में आदमी अधिक बोलने के कारण ग्रस्त होता है। जब ज़्यादा बोलने और बोलते रहने की आदत आदमी को हो जाती है तो सही और ग़लत का विचार बहुत कम रहता है। बात को सुन्दर बनाने के लिए बहुत-सी निराधार बातें भी उसे गढ़नी पड़ती हैं। साधारणतया यह देखा गया है कि ज़्यादा बोलने वालों की बातें तुच्छ और बकवास होती हैं। परनिन्दा, दुष्भाषिता और झूठ बोलने के अपराधी भी वे अधिकतर हो जाते हैं।
मितभाषिता और ख़ामोशी जब किसी का स्वभाव होगा तो वह जो कुछ भी कहेगा सोचकर और सत्य की तुला में तौलकर कहेगा। फिर ग़लती और गुनाह की सम्भावना भी कम से कम रहेगी। ज़्यादा बोलने से बोलनेवाले की गरिमा घट जाती है। वह स्वयं अपने व्यवहार से अपनी बातों का मूल्य घटाता है। मूल्यवान वस्तु आदमी इस प्रकार अन्धाधुन्ध तो ख़र्च नहीं करता बल्कि सोच-समझकर और अवसर देखकर करता है।
कम बोलने के कारण आदमी सोच-विचार करने की स्थिति में होता है। सोच-विचार के पश्चात वह जो कुछ मुख से निकालेगा उसमें वज़न होगा और लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा।
ज़्यादा बोलनेवाले साधारणतया यह नहीं देख पाते कि कौन-सी बात कहने की है और कौन-सी बात कहने की नहीं है। कभी सुननेवालों की रुचि मात्र और उनकी माँग का तुष्टिकरण ही उनका पेशा बन जाता है। वे यह नहीं देखते कि जिस रुचि और माँग की तुष्टि वे करते चले जा रहे हैं वह सुरुचि है या विकृति और उनकी माँग सही है या ग़लत। इस प्रकार के अनावश्यक रूप से अधिक बोलनेवालों के लिए अल्लाह की किताब और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन दुष्कर होता है। इसलिए कि उनकी सस्ती भावनाओं की सन्तुष्टि का सामान तो अनर्गल भाषण में होता है। उनकी बिगड़ी हुई लत दूसरे लोगों की अभिरुचि को भी बिगाड़ देती है। नतीजा यह होता है कि दूसरे भी उनके प्रभाव में आकर क़ुरआन पाठ और अध्ययन, विचार और चिन्तन से वंचित रह जाते हैं। व्यर्थ बोलनेवालों की श्रेणी में वे पत्रकार और स्तम्भकार भी आते हैं जो साहित्य की इस्लामी अभिरुचि को जिसका उत्तम नमूना क़ुरआन और हदीस के रूप में हमारे सामने है, आहत करते हुए लोगों की सस्ती और अशिष्ट भावनाओं से खेलने और अपना रंग जमाने की कुचेष्टा करते हैं।
ख़ामोशी की दौलत पाकर आदमी इन तमाम आपदाओं से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार शैतान को अपने से दूर करने में उसे पूरी सफलता प्राप्त होती है।
नकारात्मक रूप से ही नहीं, सकारात्मक रूप से भी यह ख़ामोशी धर्म में आदमी की सहायक सिद्ध होती है। उसे विचार और चिन्तन का अवसर मिलता है। फिर वह बोलता है तो उसका बोलना ज़िक्र (सत्य-स्मरण) बन जाता है। वाणी ज़िक्र उसी सूरत में बनती है जब सम्त (अर्थात मौन) फ़िक्र (या विचार) बन जाए। जहाँ वाणी ही वाणी हो वहाँ सर्वप्रथम तो ज़िक्र सिरे से पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि स्वयं ज़िक्र के लिए सम्त (मौन) अपेक्षित है। दूसरे जहाँ वाणी ही वाणी है वहाँ अगर ज़िक्र होगा भी तो वह निर्जीव होगा।
ज़्यादा बोलनेवाला इसका अवसर ही शेष नहीं रहने देता कि परोक्ष से उसपर अनुग्रह-वर्षा हो और उसका हृदय ज्ञान और प्रज्ञा का स्रोत बन जाए। संयम और ख़ामोशी जिनका स्वभाव और नियम होता है उन्हीं के हृदय में तत्वज्ञान उगता है, अर्थात उनपर दीन के रहस्यों का उद्घाटन होता है। जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता है। उन्हें निर्णय-शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर उनका समर्थक और सहायक होता है। ईश्वर का यह मार्गदर्शन उसे बौद्धिक और वैचारिक समस्याओं से लेकर कर्मभूमि तक प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार एक ख़ामोशी अगणित बरकतों और भलाइयों की निमित्त है। सच कहा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कि "ख़ामोशी दीन के मामले में तुम्हारी सहायक है।"
व्यर्थ बोलनेवाले की मिसाल उस नादान व्यक्ति की-सी है जो इधर-उधर की ख़बरें लेता फिरता हो और कभी भूलकर भी अपनी ख़बर नहीं लेता। ख़ामोशी इख़्तियार करना आदमी की ख़ुद अपने आप से मुलाक़ात की हैसियत रखता है। इससे ईश्वर की ओर पूर्णरूपेण एकाग्रचित होने का उसे अवसर प्राप्त होता है। ईमानवालों के यहाँ मौनधारण उच्छिन्नता और मूल्यहीनता का पर्याय कदापि नहीं है। ईमानवालों का मौन सत्यबोध से सुसज्जित है किन्तु मौन के आनन्द से अपरिचित लोग इसे कम ही समझ पाते हैं।
हँसी-मज़ाक़ की आदत वास्तव में इनसान की बेपरवाही को दर्शाती है। अत्यधिक हँसी-मज़ाक़ जैसा व्यसन हृदय को कठोर बना देता है। कठोर-हृदयता वास्तव में हृदय की मृत्यु है। मृत्यु से जिस प्रकार आदमी का शरीर निष्प्राण हो जाता है उसी प्रकार हृदय के मृतप्राय हो जाने के बाद भलाई और बुराई की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। जीवन के सूक्ष्म और कोमल संकेतों और यथार्थ को समझने की योग्यता का भी लोप हो जाता है। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“वे लोग जो ईश्वर से बहुत अधिक दूर हैं, कठोरहृदयी हैं।"
हृदय की विभिन्न अवस्थाओं और दशाओं का प्रभाव चेहरे से भी प्रकट होता है। हृदय की मृत्यु चेहरे की आभा भी छीन लेती है। चेहरे का आकर्षण जाता रहता है। वह गरिमाहीन हो जाता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं कि अल्लाह तुझे प्रत्येक दुविधा से मुक्ति दे और तेरे अन्दर वह साहस पैदा हो जाए कि तुझे कोई भी चीज़ सत्य के प्रकट करने से रोक न सके। धिक्कारनेवाले अकारण धिक्कारते रहें किन्तु इससे निश्चिन्त होकर सदैव ईश्वर की महानता और उसके अधिकारों का तुझे ध्यान रहे। अल्लाह के दीन की सर्वोच्चता के लिए प्रयासरत रहने ही में तुझे अपनी प्रतिष्ठा दिखाई दे।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की अन्तिम नसीहत से मालूम हुआ कि लोगों में दोष निकालना कोई पवित्र कार्य हरगिज़ नहीं है। जब किसी का दोष निकालने का विचार आए तो अपने अवगुणों को देखो कि स्वयं मेरे अन्दर कितनी ही त्रुटियाँ व्याप्त हैं, मैं दूसरे के दोष क्या टटोलूँ और उसके अवगुणों को क्या उछालूँ।
शक्ति और वीरता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शक्तिशाली मोमिन अल्लाह की दृष्टि में दुर्बल मोमिन से ज़्यादा अच्छा और प्रिय है। और यूँ तो प्रत्येक में भलाई पाई जाती है। जो चीज़ तुम्हारे लिए लाभदायक हो उसके लोभी बनो और ईश्वर से सहायता की याचना करो और असमर्थ न हो और अगर तुम्हें कोई संकट आ पड़े तो यह न कहो कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि यह कहो कि अल्लाह ने यही नियत किया था और उसने जो चाहा किया। क्योंकि यह 'यदि' शब्द शैतानी कर्म का द्वार खोलता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : दुर्बल मोमिन से वह मोमिन बेहतर और अल्लाह की दृष्टि में ज़्यादा प्रिय है जो शक्तिशाली हो अर्थात किसी मामले में कमज़ोर न पड़े, जिसका ईमान सुदृढ़ हो और जिसके संकल्प में कोई भी कमज़ोरी न पाई जाती हो। जो ईश्वर पर सबसे बढ़कर भरोसा रखता हो। जो लोगों के उत्पीड़नों से बेपरवाह होकर अल्लाह के बन्दों को उनके अधिकार प्रदान करने में आगे-आगे रहे। दीनी मामलों में और लोगों को सत्य की ओर आमन्त्रित करने में कोई कठिनाई उसके संकल्प और साहस को पराजित न कर सके।
भलाई से कोई भी मोमिन रिक्त नहीं हो सकता। कमज़ोरों में भी कोई न कोई गुण अनिवार्यतः पाया जाता है जिसे धर्म के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि शक्तिशाली मोमिन का दर्जा सबसे बढ़कर होता है।
जो चीज़ लाभप्रद हो विशेष रूप से जो दीनी मामलों में लाभ पहुँचाए उसकी उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए बल्कि ऐसी चीज़ का तो आदमी को लोभ होना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसकी मदद से कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी प्राप्ति असम्भव है। इसलिए न तो किसी को वांछित वस्तु प्राप्त करने में कमज़ोरी दिखानी चाहिए और न इसके लिए ईश्वर से अपनी प्रार्थना त्यागनी चाहिए।
यह हदीस बताती है कि यह कहना कि अगर हमने ऐसा किया होता तो हम संकट में न पड़ते, उचित नहीं है। इससे आदमी साहसहीन हो जाता है और शैतान तो हमें हतोत्साहित ही देखना चाहता है। वह चाहता है कि संशयों से हम कभी मुक्त न हो पाएँ। संकट और विपत्ति के अवसर पर हमें कहना चाहिए कि ईश्वर की ओर से हमारे लिए यही नियत था। वह जो चाहता है करता है। उसकी इच्छा निरर्थक नहीं हो सकती। हम उसके निर्णय पर राज़ी हैं। सारांश यह कि नियति पर आक्षेप किसी तरह भी उचित नहीं। क़ुरआन में भी आया है—
“कह दो हमें कुछ भी पेश नहीं आ सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया। वही हमारा प्रभु है। और ईमानवालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।" (9:51)
मालूम हुआ कि जहाँ दुख व्यक्त करना व्यर्थ हो वहाँ दुख व्यक्त करना अनुचित है। ऐसे अवसर पर मनुष्य को ईश्वर के निर्णय पर राज़ी होना चाहिए। अलबत्ता अगर ईश्वर के आज्ञापालन में किसी कोताही पर खेद हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह खेद और क्षोभ भविष्य के लिए एक चेतावनी का काम दे सकता है। मगर इस खेद की भी एक सीमा है। इस खेद को इतना आगे न बढ़ने दिया जाए कि आदमी इसी में घुलता रहे और किसी काम का न रह जाए। अपनी ग़लती का एहसास हो जाने पर आदमी क्षमायाचना से काम ले और भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प करे कि वह धार्मिक मामलों में किसी लापरवाही और सुस्ती से काम न लेगा।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कौन मुझसे यह तलवार लेगा? और इसको वह व्यक्ति ले जो इसका हक़ अदा करे।” फिर उसको अबू-दुजाना ने ले लिया। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : उहुद के युद्ध के अवसर पर जबकि सत्य और असत्य के बीच सख़्त मुक़ाबला पेश आया था, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हाथ में एक तलवार लेकर कहा था कि इसे कौन लेगा? कितने ही हाथ उसे लेने के लिए बढ़े। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि इसे वही व्यक्ति ले जो इसका हक़ अदा कर सके। अर्थात जो अत्यन्त वीरता दिखाए। मालूम हुआ कि सत्य और असत्य के संघर्ष में वीरता ही काम आती है। इसी लिए धर्म में वीरता को विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
उत्तरदायित्व
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कभी बन्दा ईश्वर की प्रसन्नता की कोई बात कहता है और वह उसके महत्व और गरिमा को नहीं जानता, जबकि उसके कारण ईश्वर उसके दर्जों को उच्चता प्रदान करता है। और कभी कोई बन्दा ज़बान पर ऐसी बात लाता है जो ईश्वर को क्रोधित करनेवाली होती है और उसमें उसे कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती जबकि वह उसके कारण नरक में जा गिरता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ऐसा होता है कि किसी आदमी को इसका अनुमान भी नहीं हो पाता कि उसे जो बात कहने का अवसर मिला है वह बात कितनी बहुमूल्य है। ईश्वर की प्रसन्नता की बात, अर्थात ऐसी बात जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है, कहने से उसके दर्जे उच्च हो जाते हैं। किसी के मुख से निकली हुई बात वास्तव में उस व्यक्ति की हैसियत निश्चित करती है। हम जानते हैं कि ईश्वर उन्हीं बातों से प्रसन्न हो सकता है जो अनुचित और गिरी हुई न हों। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता की बात करनेवाला व्यक्ति गिरा हुआ नहीं रहेगा। उसके दर्जे उच्च होंगे और उसे दर्जों की ये उच्चता उस बात के मूल्य के अनुसार प्राप्त होती है। उसके दर्जों को उच्च करनेवाला कोई और नहीं स्वयं ईश्वर होता है। अब यह बन्दे की ज़िम्मेदारी होती है कि ऊँचाई से गिरकर वह फिर पस्ती में न जा पड़े।
कभी ऐसा होता है कि आदमी की बात अत्यन्त ग़लत, अनुचित और ईश्वर के क्रोध को भड़कानेवाली होती है किन्तु उसे उसकी बुराई का कुछ भी एहसास नहीं होता। और यह चीज़ उसे ले डूबती है। वह नरक में गिर जाता है।
एक हदीस में ये शब्द आए हैं—
"वह बात उसे जहन्नम की आग में इतनी दूरी पर डाल देती है जितनी दूरी पश्चिम और पूर्व के मध्य पाई जाती है।"
अर्थात वह जहन्नम की अत्यन्त गहराई में जा गिरता है।
(2) हज़रत बिलाल-बिन-हारिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी कभी कोई भली बात मुख से निकालता है और वह उसके मूल्य और दर्जे को नहीं जानता हालाँकि उसके कारण ईश्वर अपनी प्रसन्नता उसके लिए उस दिन तक के लिए लिख देता है जबिक वह उससे मुलाक़ात करेगा। और आदमी कभी कोई बुरी बात ज़बान पर लाता है वह उसकी वास्तविकता को नहीं जानता हालाँकि उसके कारण ईश्वर उसपर अपने प्रकोप को उस दिन तक के लिए वाजिब कर देता है जबकि वह उससे मिलेगा।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह, मालिक, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : ईश्वर की यह प्रसन्नता और ईश्वर की यह रज़ामन्दी कोई सामयिक और अस्थायी चीज़ नहीं होती, क़ियामत तक के लिए वह उससे राज़ी हो जाता है। और इसके बाद तो वह ईश्वर के स्वर्ग का अधिकारी होता ही है। इस हदीस की व्याख्या में यह भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया में नेकी का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह क़ब्र की आज़माइशों से मुक्त होता है। उसकी क़ब्र आलोकित और विस्तृत कर दी जाती है। फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि उस दुलहन की भाँति निद्रामग्न हो जाओ जिसको उसके लोगों में से सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति ही जगा सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर उसे उसके शयनस्थल से उठाएगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)
अलबत्ता जिसपर ईश्वर क्रोधित हुआ उसका मामला उस व्यक्ति के विपरीत होगा जिस व्यक्ति की प्रिय बात के कारण ईश्वर उससे प्रसन्न होगा।
इस हदीस में यह जो कहा गया कि, “उस दिन तक के लिए जबकि वह ईश्वर से मिलेगा" तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि प्रसन्न या क्रोधित होने का सिलसिला बस क़ियामत तक के लिए ही है, उसके बाद इस सिलसिले का अन्त हो जाएगा। ईश्वर का जो निर्णय जिस किसी के लिए होगा वह तो आख़िरत में यथावत ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क़ुरआन में शैतान के बारे में कहा गया है—
“और निश्चय ही बदला दिए जाने के दिन तक तुझपर मेरी लानत है।" (38:78)
स्पष्ट है कि बदला दिए जाने के दिन के बाद यह लानत ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि अभिप्राय यह है कि क़ियामत तक तो फिटकार और लानत उसपर बरसती रहेगी और उसके बाद लानत के साथ वह यातनाग्रस्त भी होगा ताकि वह अपने अपराध का दंड भी भुगते।
वैचारिक परिपक्वता
(1) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम इम्मअः न बनो कि कहने लगो कि लोग नेकी और भलाई करेंगे तो हम भी नेकी और भलाई करेंगे और अगर वे अत्याचार करेंगे तो हम भी अत्याचार करेंगे। बल्कि अपने दिलों को टिका दो, अगर लोग नेकी करें तो तुमपर अनिवार्य है कि नेकी करो, और अगर वे बुराई करें तो तुम अत्याचार न करो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इम्मअः एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने मत पर दृढ़ न हो बल्कि अक़्ल में दूसरों के अधीन होकर रहे।
यह हदीस बताती है कि यह नीति कदापि उचित नहीं है कि तुम्हारा निर्णय दूसरों के निर्णय पर निर्भर करे और तुम यह कहो कि लोग हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारा भी उनके साथ होगा, बल्कि तुम्हारा अपना कोई मत और सोची-समझी नीति होनी चाहिए जिसपर तुम दृढ़तापूर्वक कार्यरत रहो। ग़लतकारों की ग़लतकारी हरगिज़ पैरवी के लायक़ नहीं हो सकती।
बुराई से पेश आनेवालों के साथ तुम्हें अत्याचार की नीति कदापि नहीं अपनानी चाहिए। अगर तुमपर कोई अत्याचार करता है तो तुम सीमा से आगे न बढ़ो। अगर अत्याचार का बदला लेना ही है तो इस बात का ध्यान रहे कि बदला लेने में किसी प्रकार का ज़ुल्म और ज़्यादती कदापि वैध नहीं। इस मामले में शरीअत को पूर्णतया ध्यान में रखो। पसन्दीदा बात तो यह होगी कि अत्याचार के जवाब में क्षमा से काम लो और अत्याचार करनेवाले को माफ़ कर दो। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी किसी से व्यक्तिगत बदला नहीं लिया।
और अगर उसे तुम केवल क्षमा ही न करो बल्कि उसपर अतिरिक्त उपकार भी करो तो यह सर्वोत्कृष्ट नीति होगी और यह स्थान केवल सिद्दीक़ीन को प्राप्त हुआ करता है। क़ुरआन में भी है—
“बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, मगर जो क्षमा कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। निश्चय ही वह ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता।" (42: 40)
यह हदीस इस प्रकार भी उल्लिखित है—
“तुम में से किसी को इम्मअः (ढुलमुल) नहीं होना चाहिए कि वह कहे कि मैं तो लोगों के साथ हूँ, अगर वे अच्छा काम करेंगे तो मैं भी अच्छा काम करूँगा और अगर वे बुरा काम करते हैं तो मेरा व्यवहार भी बुरा होगा। नहीं, बल्कि अपने आप को एक बात पर क़ायम रखो। अगर लोग अच्छा काम करें तो तुम अच्छा काम करो और अगर वे बुरा काम करें तो उनकी बुराई से विलग रहो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
आज कितने ही बुरे काम लोग बिगड़े हुए समाज के बिगड़े हुए लोगों के अन्धानुकरण में करते हैं। आदमी को स्वयं प्रत्येक काम के भले-बुरे पर विचार करके एक गम्भीर निर्णय लेना चाहिए और फिर उस निर्णय पर दृढ़तापूर्वक कार्यरत होना चाहिए। अगर कोई काम बुरा है तो है। लोगों के उसे करने के बाद भी वह बुरा ही रहेगा। ऐसे काम से बचना ज़रूरी है। यही सफलता का सही रास्ता है।
इस हदीस में चरित्र-निर्माण की महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि आदमी का अपने जीवन के बारे में एक सोचा-समझा गम्भीर निर्णय हो। यह नहीं कि उसका अपना कोई संकल्प और निर्णय ही न हो और वह दूसरों के पीछे दौड़ने पर विवश हो। ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होगा। चरित्र के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य की विभिन्न इच्छाओं में एकत्व स्थापित हो और उसके कर्म उसी एकत्व को प्रतिबिम्बित करते हों। Ospunskey ने यह बात बहुत सही कही है कि जब तक मानव इस प्रकार का ऐक्य स्थापित न कर ले उसे अपने आप को 'मैं' कहने का कोई अधिकार नहीं। उसका तो अपना कोई इरादा ही नहीं है। इरादा हमेशा इच्छाओं का परिणाम होता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएँ किसी स्थाई और शाश्वत मूल्य के अधीन न हों वह अपनी भावनाओं और बाह्य प्रभावों का खिलौना मात्र होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन मात्र संयोगों द्वारा परिचालित होता है। उसे कुछ ख़बर नहीं होती कि आइंदा वह क्या क़दम उठाएगा और दूसरी ही साँस में उसके मुख से कौन-सी बात निकलेगी।
जब तक जीवन में समरसता और एकत्व उत्पन्न न हो समाज में भी समरसता और एकता सम्भव नहीं। चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करने और इच्छाओं और भावनाओं में ऐक्य व समरसता स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें दरकार हैं—
(i) जीवन के कुछ स्थाई और शाश्वत मूल्य हों और आदमी को उनका ज्ञान हो और वह उनपर ईमान लाए।
(ii) जीवन का कोई बुनियादी लक्ष्य हो जो भौतिकता और सामान्य उपयोगिता के दृष्टिकोण से उच्च हो। जगत् और जगत् में पाई जानेवाली वस्तुओं की हैसियत वास्तव में ऐसे साधन और माध्यम की है जिसके द्वारा मानव की आत्मा अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
(iii) इस सम्बन्ध में तीसरी अपेक्षित चीज़ यह है कि मानव का जीवन की निरन्तरता पर विश्वास हो। चिरस्थाई जीवन के बिना स्थाई और शाश्वत मूल्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्ति इसपर विश्वास न रखता हो कि उसके विचार और कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं उस समय तक किसी सुदृढ़ चरित्र व व्यक्तित्व की आशा नहीं की जा सकती। जिस समाज के व्यक्तियों का अन्तिम उद्देश्य निकटस्थ और त्वरित लाभ की प्राप्ति हो, उनसे किसी महान व्यक्तित्व की आशा नहीं की जा सकती।
(iv) इन समस्त बुनियादी चीज़ों का अस्तित्व ईश्वर के बिना सम्भव नहीं। इसलिए कि चरित्र और व्यक्तित्व में दृढ़ता उसी स्थिति में आ सकती है जबकि यह विश्व बिना ईश्वर के न हो। ईश्वर ने मानव को सोद्देश्य जीवन प्रदान किया हो और जीवन के शाश्वत मूल्यों से उसे परिचित कराया हो, और इससे अवगत कराया हो कि सांसारिक जीवन ही जीवन नहीं है। मानव शाश्वत जीवन का अधिकारी हो सकता है अगर वह ईश्वर-निर्धारित जीवन-लक्ष्य से विचलित न हो बल्कि अपने को उच्च नैतिकता और चरित्र का पाबन्द बनाए।
नबियों का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि वे मानव जीवन के लिए समस्त अपेक्षित चीज़ें उपलब्ध कर देते हैं जो चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अतएव मानव का कर्तव्य है कि वह नबियों की शिक्षओं को अपनाए और स्वयं को और अपने समाज को कामयाब बनाने की कोशिश करे। जो लोग नबियों की शिक्षाओं पर ईमान रखते हैं उनके ईमान के लिए अपेक्षित है कि उनका व्यक्तित्व सुदृढ़ हो। ग़ाफ़िल और भटके हुए लोगों के पीछे चलने के बजाय वे हमेशा सत्य का अनुसरण करें और उस चरित्र को हरगिज़ दाग़ न लगने दें जो उनके ईमान का परिचायक है। लोग अगर जीवन में सही कार्यनीति अपनाते हैं तो वांछित भी यही है, लेकिन अगर वे ग़लत कार्यनीति अपनाते हैं तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक अवस्था में भलाई और नेकी के मार्ग पर चलना है।
समाज के लोगों में साधरणतया यह कमज़ोरी पाई जाती है कि लोग एक-दूसरे की कमज़ोरियों को अपने लिए बहाना बनाते हैं कि अमुक व्यक्ति पीछे है तो हम क्यों सत्य की सेवा में आगे बढ़ें। अमुक व्यक्ति तो त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी जान क्यों खपाएँ। अमुक व्यक्ति तो व्यवसाय में नाजायज़ तरीक़ा अपनाकर अपनी आमदनी में असाधारण वृद्धि कर रहा है, आख़िर हम क्यों अपने को वंचित रखें। यह विचारशैली ईमानवालों की नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति तो अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर देता है कि वह अभी तक ईमान की आत्मा से अपरिचित है। अभी ईमान उसके दिल में ठीक से उतरा ही नहीं।
इस हदीस के ये शब्द हृदयंगम कर लेने योग्य हैं कि “अपने दिल को एक चीज़ पर अटका दो।" अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी दशा उस लुटे-पिटे व्यक्ति की होगी जिसका कोई वतन न हो। जो बेघर होकर इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा हो। ईश्वर ने हमें जो सिद्धान्त और अवधारणाएँ प्रदान की हैं उनकी हैसियत हमारी आत्मा के लिए एक बेहतरीन ठिकाने और वतन की है। हमें उसी वतन की नागरिकता अपनानी चाहिए।
दृढ़ता और अडिगता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम अमल अपनी शक्ति के अनुसार करो क्योंकि ईश्वर (बदला देने में) नहीं थकता जब तक कि तुम (अमल करते-करते) न थक जाओ। तुम यह नीति इसलिए भी अपनाओ कि ईश्वर को वह कर्म प्रिय है जिसे निरन्तर किया जाए, यद्यपि वह थोड़ा हो।” और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब कोई कर्म करते तो हमेशा उसकी पाबन्दी करते। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : आदमी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिहाज़ से ही उत्तरदायी है। उसे अपने कर्मों में वही कार्यशैली अपनानी चाहिए जो उसके चरित्र की परिचायक हो सके। सामयिक आवेश में आकर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने लग जाता है जिसकी शक्ति और सामर्थ्य उसमें नहीं होती। वह देर तक इसे कर नहीं सकता। इसलिए इबादत और संयम इत्यादि उतना ही पसन्दीदा है कि जितना आदमी उसे स्थायी रूप से अपना सके।
ईश्वर बदला देने में नहीं थकता लेकिन आदमी कर्म करने से थक सकता है। इसलिए उसे अपनी ताक़त को देखते हुए अमल करना चाहिए ताकि उसके लिए उसकी पाबन्दी सम्भव हो सके। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत और तरीक़ा यही रहा है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किसी अमल को शुरू करते तो उसे त्यागते नहीं थे।
एक मौक़े पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कर्मों में से जितना कर सको उतना ही करो क्योंकि ईश्वर नहीं थकता बल्कि तुम ही थक सकते हो।”
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह के निकट प्रियतर कर्म वह है जो सदैव किया जाए यद्यपि वह थोड़ा ही हो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : जो कर्म नियमित रूप से किया जाता है वही कर्म विश्वसनीय होता है। इसलिए कि आदमी का वास्तविक कर्म वही है जिसे वह निरन्तर रूप से करता है, वही उसके चरित्र का असली परिचायक होता है। फिर जो कर्म स्थायी रूप से किया जाता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो, उसी का शुभ परिणाम भी सामने आता है। जिस काम को करके आदमी हमेशा के लिए या लम्बे समय के लिए छोड़ दे उससे किसी ख़ास नतीजे और प्रभाव की आशा भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि आदमी का असली कर्म वही है जो उसने बेदिली के साथ नहीं बल्कि प्रसन्नता और आनन्द के साथ किया हो। क्योंकि इसके बिना हम वास्तव में कर्म के साथ न होकर कहीं और ही होते हैं। इसी लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है कि तुममें से कोई जब तक ख़ुशदिली के साथ नमाज़ पढ़ सके पढ़े, जब सुस्त हो जाए तो उसे बैठ जाना चाहिए।
(3) हज़रत सुफ़ियान-बिन-अब्दुल्लाह सक़फ़ी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसुल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इस्लाम के बारे में आप मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि फिर आप के बाद इसके विषय में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़े। एक उल्लेख में ये शब्द आए हैं कि फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सिवा किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता मुझे न हो। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, कहो, “कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इसी पर जमे रहो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत सुफ़ियान-बिन-अब्दुल्लाह सक़फ़ी का आशय यह था कि उन्हें ऐसी बात बता दी जाए जो इतनी संग्राहक और सारगर्भित हो कि वही इस्लाम का सारांश हो और वही उनके लिए जीवन का मार्गदर्शन हो जाए। फिर उन्हें इस्लाम की वास्तविकता को समझने और उसकी प्रकृति और उसकी आत्मा के अनुसार जीवन की दिशा निर्धारित करने और चरित्र व व्यक्तित्व के निर्माण के सम्बन्ध में किसी से कुछ और अधिक मार्गदर्शन प्राप्त करने की कभी कोई आवश्यकता न पड़े।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के उत्तर से ज्ञात हुआ कि ईमान-बिल्लाह अर्थात एक ईश्वर पर ईमान ही इस्लाम का सारांश है। बाक़ी जितनी अवधारणाओं और आदेशों की शिक्षा इस्लाम में दी गई है वह वास्तव में एक ईश्वर पर ईमान लाने की अपेक्षा और अनिवार्यता है। ईश्वर पर ईमान अर्थात उसकी प्रभुता, पूजनीयता और प्रियता को स्वीकार कर लेने के पश्चात जीवन वह रूप धारण कर लेता है जिससे श्रेष्ठ और सुन्दर और शान्तिमय जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही जीवन है जिसे मोमिन का जीवन कहा जाता है।
इस हदीस में जो बात कही गई है वह ईश्वर की किताब क़ुरआन से उद्धृत है। क़ुरआन में है—
“निश्चय ही जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वे उस पर जमे रहे तो उन्हें न कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे।” (46: 13)
वास्तव में जिस चीज़ को जीवन कहते हैं वह बस यही है कि मानव अपने जीवन स्रोत अर्थात अपने ईश्वर को पहचाने। उसका सम्बन्ध ईश्वर ही से हो। वही उसकी समस्त कामनाओं का केन्द्र बिन्दु हो। वही उसके शौक़ की पनाहगाह हो। उससे मिलने की आकांक्षा ही में वह जीता हो और उसी के लिए वह ख़ाक में मिलने की तमन्ना रखता हो। उसी की प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा उसे कर्मभूमि में सक्रिय रखती हो। उसी की महानता और बड़ाई से वह दुनिया को परिचित कराने के लिए प्रयासरत हो। उसी के आदेशों के क्रियान्वित होने की कामना उसे असत्य से लोहा लेने पर उभारती हो। क़ुरआन में है—
“वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और सांसारिक जीवन ही पर निहाल हो गए हैं और उसी पर सन्तुष्ट हो बैठे और जो हमारी निशानियों की ओर से ग़ाफ़िल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है, उसके बदले में जो वे कमाते रहे।" (10:7-8)
इसमें सन्देह नहीं कि ईश-मिलन की कामना मोमिन के लिए जीवन-उष्मा की भाँति है। यही उसकी शक्ति और यही उसके जीवन की निधि है।
क्रोध पर नियन्त्रण
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी बन्दे ने कोई घूँट ऐसा नहीं पिया जो प्रतापवान अल्लाह की दृष्टि में क्रोध के उस घूँट से श्रेष्ठ हो जिसे वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पी जाए।” (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : ग़ुस्से का परिणाम अत्यन्त घातक होता है, इसी लिए ग़ुस्से का घूँट पीना ईश्वर की दृष्टि में दूसरी प्रत्येक चीज़ के घूँट पीने से बेहतर है, शर्त यह है कि यह घूँट आदमी केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पिए। इसका कोई दूसरा प्रेरक न हो। ग़ुस्से को वही व्यक्ति नियन्त्रित कर सकता है जो लोगों की ग़लती और उनके अत्याचार को क्षमा कर सकता हो और जिसे ईश्वर की प्रसन्नता दुनिया की प्रत्येक वस्तु से बढ़कर प्रिय हो। क़ुरआन में परहेज़गार व्यक्तियों के गुणों के प्रसंग में कहा गया है—
“और वे क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं।" (3:134)
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि आप मुझे नसीहत करें। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्रोध न कर।" उस व्यक्ति ने कई बार यही निवेदन किया और हर बार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यही कहा कि क्रोध न कर। (हदीस : बुख़ारी, मुवत्ता)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रत्येक व्यक्ति को उसके सवाल का जवाब उसकी स्थिति के अनुसार देते थे। प्रार्थी में क्रोध की अधिकता थी। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे क्रोध न करने का निर्देश दिया। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि क्रोध में अकसर लोग अपना सन्तुलन खो देते हैं और उन्हें मर्यादाओं का भी कुछ ध्यान नहीं रह पाता। क्रोध में मुख से अशोभनीय बातें तो निकलती ही हैं। आदमी कभी-कभी इससे बढ़कर ऐसा क़दम भी उठा लेता है जिसके अत्यन्त घातक परिणाम सामने आते हैं। अगर आदमी कोई ऐसा क़दम न भी उठाए तो भी उसका हृदय कपट और द्वेष से भर ही जाता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यह नसीहत ऐसी है कि अगर कोई इसका पालन करे तो वह शीघ्र ही नैतिक गुणों की प्रतिमूर्ति बन सकता है। ग़ुस्सा आने पर हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर का प्रकोप और क्रोध तो सबसे बड़ा है फिर भी वह क्षमा से काम लेता है। कितने ही लोग दिन-रात उसकी अवज्ञा करते रहते हैं लेकिन वह क्षमा करता है और उनकी अवज्ञा पर उन्हें शीघ्र ही नहीं पकड़ता।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शक्तिशाली पहलवान वह नहीं है। जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि शक्तिशाली पहलवान तो वास्तव में वह है जो क्रोध के समय स्वयं को नियन्त्रण में रखे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में क्रोध में धैर्य और सहनशीलता से काम लेनेवालों की प्रशंसा की गई है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि शरीअत का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि आदमी को किसी बात पर क्रोध आए ही नहीं। अनुचित बातों पर क्रोध आना स्वाभाविक है। शरीअत का वास्तविक उदद्देश्य यह है कि क्रोध में आदमी सीमाओं का उल्लंघन कदापि न करे बल्कि इस अवस्था में भी उसे अपने आप पर पूरा नियन्त्रण हो। वह क्रोधवश ऐसे कार्य न करे जो मोमिन के मर्यादानुकूल नहीं होतीं।
(4) हज़रत सहल-बिन-मआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति क्रोध को पी जाए, जबकि उसे इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि अपना क्रोध उतार सकता है और उसके तक़ाज़े को पूरा कर सकता है, अल्लाह उसे क़ियामत के दिन सम्पूर्ण सृष्टि-जन के सामने बुलाएगा। यहाँ तक कि उसको अधिकार देगा कि वह जिस हूर को भी चाहे अपने लिए चुन ले।” (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : सम्पूर्ण सृष्टि-जन के सामने बुलाने का अर्थ यह है कि ईश्वर लोगों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, उसे प्रसिद्धि देगा और उसपर गर्व करेगा।
ग़ुस्सा आने पर कोई जवाबी कार्रवाई न करना जबकि आदमी को इसकी पूरी शक्ति प्राप्त हो इससे उसके जिस व्यक्तिगत और नैतिक सौन्दर्य का पता चलता है इसे दृष्टिवान भली-भाँति समझ सकते हैं। जब उस व्यक्ति ने जीवन में नैतिक सौन्दर्य को, जो वास्तव में जीवन का वास्तविक सौन्दर्य और शोभा है, पसन्द किया तो इसका प्रतिदान वही कुछ होना चाहिए जिसका उल्लेख इस हदीस में किया गया है। ईश्वर उससे कहेगा कि तुमने दुनिया में निकृष्टतम नीति न अपनाकर अपने नैतिक सौन्दर्य का परिचय दिया है तो अब यहाँ भी पूरी आज़ादी से जन्नत की जिस ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत हूर (अप्सरा) को चाहो अपने लिए चुन लो। कर्म और उसके प्रतिफल में सादृश्यता और सामंजस्य तो होना ही चाहिए।
इस हदीस में क्रोध पी जानेवाले व्यक्ति के उच्च स्थान का वर्णन है। और अगर कोई व्यक्ति क्रोध के नियन्त्रण के साथ ही अपने विरोधी पर उपकार भी करे तो उसका क्या स्थान होगा यह हमें स्वयं सोचना चाहिए।
(5) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुममें से किसी व्यक्ति को ग़ुस्सा आए तो चाहिए कि वह बैठ जाए। फिर अगर ग़ुस्सा ठण्डा हो जाए तो ठीक, अन्यथा चाहिए कि लेट जाए।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह क्रोध पर नियन्त्रण का मनोवैज्ञानिक उपाय है। ग़ुस्से में आदमी से जो अनुचित और अनर्गल कृत्य होते हैं बैठ जाने पर उनकी सम्भावना बहुत ही कम शेष रहती है। और अगर वह लेट जाए तो इस हालत में तो स्वभावतः उसका असभ्य व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। आशा है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बताए हुए इस उपाय से आदमी अपने ग़ुस्से पर आसानी से क़ाबू पा लेगा।
(6) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लोगों को शिक्षा दो और आसानी पैदा करो, कठिनाई न उत्पन्न करो। जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले, और जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले, और जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तबरानी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बात का अर्थ यह हुआ कि लोगों को दीन की शिक्षा दो और उन्हें धर्म की अनिवार्यताओं से अवगत कराओ लेकिन यह तथ्य हमेशा सामने रहे कि सत्य-धर्म का वास्तविक उद्देश्य लोगों को मुश्किलों और कठिनाइयों में डालना कदापि नहीं है, बल्कि वह तो उन्हें कठिनाइयों और विपत्तियों से छुटकारा दिलाने आया है। (7:157)
इसलिए शिक्षा और इस्लामी आह्वान की नीति यह है कि लोगों के सामने दीन की शिक्षाएँ इस प्रकार प्रस्तुत की जाएँ कि वे उन्हें कष्टकर नहीं बल्कि हितकर समझें। दीन उन्हें एक अप्रिय बोझ और एक दुर्गम घाटी प्रतीत न हो जिसे पार करना उन्हें कठिन ही नहीं असम्भव नज़र आए।
क्रोध आने पर मौन धारण करना क्रोध पर नियन्त्रण का एक उत्तम व्यावहारिक उपाय है। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार यह बात कही कि जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले।
क्रोध की अवस्था में आदमी जब मुँह खोलेगा तो इसकी पूरी सम्भावना है कि वह अपने ग़ुस्से पर क़ाबू न पा सके, क्योंकि जब वह प्रतिक्रिया में कुछ कहेगा तो दूसरा पक्ष भी चुप नहीं रह सकता, वह भी कुछ न कुछ कहेगा। इससे ग़ुस्सा और भड़केगा, और बात मार-काट तक पहुँच सकती है। और फिर आपस के सम्बन्धों के सुधरने की सम्भावनाएँ बहुत ही कम शेष रह जाएँगी।
धैर्य
(1) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अनसार में से कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कुछ माँगा तो आपने उन्हें दिया। उन्होंने फिर माँगा तो आप ने उन्हें दिया। उन्होंने फिर माँगा तो आपने उन्हें दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था समाप्त हो गया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “मेरे पास जो भी माल होगा मैं तुमसे बचाकर उसे नहीं रखूँगा, और जो कोई सवाल से बचना चाहता है ख़ुदा उसे माँगने (की हीनता) से बचा लेता है और जो कोई सम्पन्नता चाहता है ईश्वर उसे सम्पन्न कर देता है और जो व्यक्ति धैर्य अपनाना चाहता है तो ईश्वर उसे धैर्य प्रदान कर देता है। और धैर्य से उत्तम व समाईवाला कोई उपहार किसी को प्रदान नहीं किया गया।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बड़े दानशील थे। इसी लिए कहा कि मेरे पास जो कुछ होगा मैं तुमसे कुछ भी उठाकर नहीं रख सकता। माँगोगे तो तुम्हें वंचित नहीं रखूँगा। लेकिन इसी के साथ आपका सर्वाधिक प्रयास यह था कि आपके साथी नैतिक गुणों से युक्त हों। उनमें चरित्र और नैतिकता की दृष्टि से कोई दोष न पाया जाए। उनके प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपने जो शिक्षा उन्हें दी वह उस समय दी जबकि आपका हाथ ख़ाली था। उन्हें देने को आपके पास कुछ न था, ताकि किसी के दिल में शैतान यह संशय न उत्पन्न कर सके कि यह धैर्य और निरपेक्षता की शिक्षा कुछ न देने का एक बहाना है।
संयम, निरपेक्षता और धैर्य उत्तम नैतिक गुण हैं लेकिन ये गुण आदमी में उस समय उत्पन्न होते हैं जबकि उसे इनके महत्व और मूल्य का सही एहसास हो और वह इन गुणों को अपने अन्दर पैदा करने की इच्छा भी रखता हो और उसे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा हो कि वह बन्दे का वास्तविक अभिभावक है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वह किसी को दूसरों से निरपेक्ष और इन उच्च गुणों से सुसज्जित कर दे।
यह वाक्य कि धैर्य से उत्तम और अधिक समाईवाली कोई अन्य वस्तु किसी को प्रदान नहीं की गई, अत्यन्त संग्राहक वाक्य है। जिस किसी को सब्र की दौलत मिल गई तो समझ लो कि वह सर्वोत्तम वस्तु का मालिक हो गया जो समस्त भलाइयों और गुणों और प्रशंसनीय वस्तुओं को अपने अन्दर समेट लेनेवाली है। अगर किसी को धैर्य की शक्ति प्राप्त हो गई तो फिर दूसरे गुणों की उपलब्धता उसके लिए दुष्कर नहीं रही। वह जीवन की मूल प्रवृत्ति से परिचित हो गया। धैर्य के बिना जीवन के सर्वोच्च मूल्य और मान्यताएँ कभी हाथ नहीं आतीं। क़ुरआन में है—
"और यह चीज़ केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो धैर्य से काम लेते हैं और यह चीज़ केवल उसको प्राप्त होती है जो बड़ा भाग्यशाली होता है।" (41:35)
धैर्य के बिना किसी उच्च सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्कृष्ट जीवन में धैर्य दूसरे गुणों के साथ एक सौन्दर्यबोध बनकर उभरता है जिसपर किसी दूसरी वस्तु को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। धैर्य से हर प्रकार की तंगी दूर हो जाती है। इससे मन और विचार, कर्म और प्रयत्न में व्यापकता आती है। धैर्य अपना मददगार स्वयं होता है। भौतिक आवश्यकताओं को कदापि इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि नैतिक मूल्यों का बोध ही शेष न रहे।
(2) हज़रत अबू-मालिक अशअरी से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“स्वच्छता आधा ईमान है और ‘अलहम्दुलिल्लाह’ तुला को भर देता है, ‘सुबहानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाह’ जो कुछ आकाश और धरती के बीच है उसको भर देते हैं। नमाज़ प्रकाश है, सदक़ा (दान) दलील और प्रमाण है, धैर्य आलोक है और क़ुरआन तुम्हारे पक्ष में या तुम्हारे विरोध में तर्क है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठता है, फिर अपने स्वयं का सौदा करता है, फिर या तो उसे स्वतन्त्र करता है या उसे विनष्ट करता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : ईमान को यह अपेक्षित है कि हमारा अन्तर्मन और बाह्य शरीर दोनों स्वच्छ हों। जिस किसी ने अपने शरीर, कपड़ों और घर को साफ़-सुथरा रखा उसने ईमान की आधी माँग पूरी कर ली। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि स्वच्छता आधा ईमान है। अब केवल यह शेष रहता है कि वह अपने बाह्य शरीर की भाँति अपने अन्तर्मन अर्थात अपने विचार, भावनाओं, और अपनी नैतिकता और चरित्र के अन्दर भी पवित्रता लाए ताकि ईमान की समस्त माँगें पूरी हो सकें।
मानव की वास्तविक सम्पत्ति, जिसका सम्बन्ध उसके जीवन और शान्ति से है, वह सत्यज्ञान है जिसकी अभिव्यक्ति 'सुब्हानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाह' के पवित्र शब्दों के द्वारा होती है। ये शब्द जिन सचाइयों को व्यक्त करते हैं उन ही सचाइयों को स्वीकार करने से मानव के लिए जगत् अर्थपूर्ण बनता है। उन ही के कारण संसार की समस्त वस्तुएँ ईश्वर की निशानियाँ ठहरती हैं।
नमाज़ प्रकाश है। जिसके जीवन में नमाज़ न हो उसका जीवन निस्तेज होगा। उसके जीवन में अन्धकार ही अन्धकार होगा। भले ही उसे इसका ज्ञान न हो। नमाज़ ही से आदमी की वास्तविक हैसियत प्रकट होती है और इसका पता चलता है कि उसने अपनी हैसियत और स्थान को पहचान लिया है। यह स्थान इतना उच्च और श्रेष्ठ है कि इससे वंचित होना कोई भी पसन्द नहीं कर सकता। बुरा हो अज्ञान और संवेदनहीनता का जो लोगों को वंचित ही नहीं रखती बल्कि उनसे हानि का एहसास भी छीन लेती है। अन्धकार वास्तव में अभाव और मृत्यु का दूसरा नाम है। इसके विपरीत प्रकाश सफलता और जीवन का लक्षण है। हमारी नमाज़ अगर सही अर्थों में नमाज़ हो तो हमारे जीवन का मार्ग कभी अन्धकारमय नहीं हो सकता। और न हम कभी अपनी मंज़िल से अपरिचित हो सकते हैं। नमाज़ के बिना हमारी यात्रा बेमंज़िल और हमारा मार्ग अन्धकार में विलीन होकर रह जाता है।
जीवन को सदैव उदारता एवं दानशीलता अपेक्षित है क्योंकि ईश्वर की दानशीलता ने उसे अस्तित्व प्रदान किया है। कृपणता मृत्यु है, किसी चीज़ की आशा जीवित से की जा सकती है, मृत से नहीं। सद्क़े से जहाँ किसी की जीवन्तता का बोध होता है वहीं सद्क़ा इस बात का भी प्रमाण है कि बन्दा अपने ईश्वर के निकटस्थ और उसकी क्षमा और निर्वाण का अधिकारी है। हम जानते हैं कि सारी प्रतिष्ठाएँ और सफलताएँ उन ही लोगों के हिस्से में आती हैं जो दान और सद्क़े के द्वारा अपने सच्चे होने का प्रमाण देते हैं।
सद्क़े का सम्बन्ध मात्र धन से नहीं है। सद्क़ा मूलतः एक चरित्र है। मोमिन भलाई के जो कार्य भी करता है वे सब सद्क़े की श्रेणी में आते हैं।
यह हदीस बताती है कि वह व्यक्ति अन्धकार में भटक रहा है जिसका जीवन धैर्य के गुण से रिक्त है। इसमें सन्देह नहीं कि सुचरित्रता से परिपूर्ण जीवन का विशिष्ट गुण धैर्य ही है।
आदमी अगर क़ुरआन के तक़ाज़ों को पहचानता और उन्हें पूरा करता है तो क़ुरआन उसकी सफलता और कल्याण की ज़मानत और उसकी मुक्ति का प्रमाण है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर क़ुरआन के अधिकारों की परवाह नहीं करता बल्कि उसके अधिकारों का निस्संकोच हनन करता है, वह न स्वयं क़ुरआन की शिक्षाओं पर चलता है और न दूसरों को क़ुरआन की ओर बुलाता है तो यही क़ुरआन उसके अपराधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है।
हदीस के अन्त में उस परिस्थिति का स्पष्ट चित्रण किया गया है जिससे हम दुनिया में दोचार हैं। हमारा हर दिन हमारे लिए यौमुल-अमल और यौमुल-जज़ा (कर्म-दिवस और प्रतिदान दिवस) दोनों बनकर आता है। प्रतिदिन हम ईश्वर की सबसे बड़ी देन अर्थात जीवन के साथ अनिवार्यतः दो में से कोई एक व्यवहार करते हैं। एक व्यवहार तो वह है जिसे अपनाकर हम स्वयं को तबाही से बचा लेते हैं और दूसरा व्यवहार वह है जो वास्तव में जीवन के साथ एक प्रकार का दुर्व्यवहार है जिसके पश्चात जीवन अपने सर्वोच्च अर्थ से वंचित हो जाता है और हम इसके भागी हो जाते हैं कि धरती से मिटा दिए जाएँ। हालाँकि प्रकटतः हम इसके बाद भी जी रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में हम विनष्ट हो चुके होते हैं। दुनिया में जब तक हम होते हैं क्षतिपूर्ति की गुंजाइश बाक़ी रहती है लेकिन जीवन समाप्त होने के साथ क्षतिपूर्ति का अवसर भी समाप्त हो जाता है।
यह हदीस सचेत करती है कि दुनिया में जीवनयापन करने का अर्थ केवल जीवन व्यतीत करना नहीं होता बल्कि यह एक प्रकार से अपने जीवन को दाँव पर लगाना होता है। इसमें सफलता या असफलता इसपर निर्भर करती है कि हम जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन ईश्वर के आज्ञापलन और बन्दगी में व्यतीत होता है या उसकी अवज्ञा और विरोध में कितने ख़ुशनसीब हैं वे लोग जिनका प्रत्येक दिन ईश्वर की प्रसन्नता चाहने में व्यतीत होता है। यही लोग हैं जिनका प्रत्येक दिन वास्तव में इस बात का उद्घोष होता है कि उन्होंने हर प्रकार की तंगी और सख़्ती और पकड़ से प्राप्त कर ली और वे हर प्रकार के विनाश से मुक्त हो गए।
धैर्य, विपत्तियों में
(1) हज़रत सुहैब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईमानवाले का मामला विचित्र है। उसका तो हर मामला उसके लिए भलाई से परिपूर्ण होता है, और यह विशेषता ईमानवाले के सिवा किसी को भी प्राप्त नहीं है। अगर उसे ख़ुशी और आराम पहुँचे तो कृतज्ञता प्रकट करता है, यह उसके लिए शुभ होता है और अगर उसपर कोई संकट आ पड़े तो वह धैर्य से काम लेता है, यह भी उसके लिए सर्वथा शुभ है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मानव-जीवन दो स्थितियों में से अनिवार्यतः किसी एक स्थिति में होता है। या तो उसे सुख-चैन प्राप्त होगा या उसे किसी दुख और विपत्ति का सामना करना पड़ रहा होगा। इनमें से जो भी हालत पेश आए ईमानवाला उससे भलाई ही समेटता है और यह विशिष्टता केवल मोमिन ही को प्राप्त होती है। ग़ैर मोमिन व्यक्ति न ख़ुशियों और सुख-चैन से कोई लाभ उठाता है और न दुख और विपत्ति से। उसे अगर सुख-चैन का जीवन प्राप्त होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। उसके जीवन में उद्दंडता और अकृतज्ञता के अतिरिक्त आप कुछ नहीं देखेंगे। उसे अगर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो वह अधीर होकर रोने-चिल्लाने लगता है। फिर शिकायत के सिवा आप उसके यहाँ कुछ नहीं पाएँगे।
लेकिन मोमिन का व्यवहार इससे बिलकुल भिन्न होता है। ख़ुशी और आराम में वह अपने ईश्वर का आभारी होता है और अगर उसपर कोई दुख या संकट की घड़ी आती है तो वह धैर्य से काम लेता है। वह समझता है कि इसमें उसके लिए कोई न कोई भलाई होगी। वह अपने प्रभु के निर्णय से सहमत होता है। यह कृतज्ञता और धैर्य वास्तव में जीवन के वे उत्कृष्ट मूल्य एवं मान्यताएँ हैं जिनके बिना हम किसी उत्तम चरित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन को अपनी सन्तान और अपने सगे-सम्बन्धियों के सम्बन्ध में दुख पहुँचता रहता है यहाँ तक कि वह अपने प्रभु से इस दशा में भेंट करता है कि उसका कोई गुनाह शेष नहीं रहता।” (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : सन्तान हो या सगे-सम्बन्धी, उनके जुदा होने का दुख स्वाभाविक है। दुनिया में दुख और शोक का यह सिलसिला जीवन के साथ लगा ही रहता है। दुनिया में इस दुख से छुटकारा नहीं। इस दुख से मोमिन भी दोचार होते हैं और ग़ैर-मोमिन भी, किन्तु मोमिन इसपर ईश्वर के लिए धैर्य से काम लेते हैं। दुख और विपत्ति को, जिसका ईमानवाले धैर्यपूर्वक सामना करते हैं, ईश्वर इसे सामान्य गुनाहों का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) बना देता है जिसका परिणाम यह होता है कि मोमिन जब दुनिया से जाता है तो वह गुनाहों के दुष्प्रभावों से बिलकुल मुक्त होता है। विपत्तियों का धैर्यपूर्वक सामना करने का प्रतिफल इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक अवसर पर कहा—
“मोमिन पुरुषों और स्त्रियों पर परीक्षा की घड़ियाँ आती रहती हैं। कभी स्वयं उसपर कोई विपत्ति आती है, कभी उसकी सन्तान पर, और कभी उसकी सम्पत्ति पर (और वह धैर्य से काम लेता है जिससे उसका हृदय स्वच्छ होता रहता है और बुराइयाँ उस से दूर होती रहती हैं) यहाँ तक कि जब वह ईश्वर से मिलता है तो उसके साथ कोई गुनाह नहीं होता।"
(3) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें से कोई व्यक्ति उस कष्ट और हानि के कारण, जो उसे पहुँची हो, मृत्यु की कामना न करे, और अगर यह कामना करना उसके लिए अवश्यंभावी हो तो उसे यह कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे उस समय तक जीवित रख जब तक जीवन मेरे लिए अच्छा हो और मुझे मौत दे उस समय जबकि मृत्यु मेरे लिए अच्छी हो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह कष्ट शारीरिक भी हो सकता है और धन-सम्पत्ति से सम्बन्धित भी हो सकता है। मृत्यु की कामना करना किसी हाल में सही नहीं है। किसी को अगर कोई हानि पहुँची है तो उसका प्रतिफल भी असाधारण है। फिर भी अगर अपरिहार्य हो तो दुआ का वह अन्दाज़ अपनाना चाहिए जिसकी शिक्षा इस हदीस में दी गई है। ईश्वर से मृत्यु माँगना तो उचित नहीं है किन्तु ईश्वरीय मार्ग में शहीद होने की अभिलाषा अच्छी है।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि—
“अल्लाह कहता है कि मेरे उस मोमिन बन्दे का मेरे पास जन्नत ही बदला है जिसके किसी प्रियतम सम्बन्धी को दुनियावालों में से उठा लूँ और वह इसपर मेरे लिए धैर्य रखे।” (हदीस : बुख़ारी)
(5) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से उल्लेख करते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बरकतवाले उच्च ईश्वर का कथन है कि ऐ आदम के बेटे! अगर तूने सदमे के प्रारम्भ में धैर्य रखा और मेरी प्रसन्नता और प्रतिदान को अपने समक्ष रखा तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम और जन्नत के सिवा किसी अन्य प्रतिदान पर सन्तुष्ट और राज़ी न होऊँगा।” (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : किसी सदमे का प्रभाव वास्तव में शुरू ही में सबसे ज़्यादा होता है। कुछ दिन बीत जाने पर तो स्वाभाविक रूप से दुख और सदमे का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी लिए सदमे के शुरू में धैर्य रखने पर ईश्वर ने प्रतिदान का वचन दिया है।
धैर्य के कारण बन्दे का अपने ईश्वर से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो जाता है कि ईश्वर यह पसन्द नहीं करता कि वह अपने उस बन्दे को जिसने उसके लिए धैर्य रखा अपनी सब से बड़ी नेमत जन्नत न दे।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अनसार की कुछ स्त्रियों से कहा—
“तुममें से जिस किसी के तीन बच्चे मर जाएँ और वह सवाब को दृष्टि में रखे (धैर्य रखे) तो वह अनिवार्यतः जन्नत में प्रवेश करेगी।" उन स्त्रियों में से एक ने कहा कि यदि दो बच्चे मरें ऐ अल्लाह के रसूल! आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यदि दो मरें (तब भी यही शुभ सूचना है)।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : बुख़ारी और मुस्लिम की एक हदीस में ये शब्द आए हैं, “तीन बच्चे जो व्यस्कता की सीमा तक न पहुँचे हों।" छोटे बच्चों से माँ का प्यार बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा होता है इसलिए उनके मरने का सदमा भी ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे माँ के बिलकुल अधीन होते हैं। वे पूर्णतया माँ ही पर निर्भर करते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि उनसे माँ को गहरा सम्बन्ध और लगाव होता है।
(7) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि उनके एक लड़के की मृत्यु हो गई तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें यह शोकपत्र लिखवाया—
“अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ओर से मुआज़-बिन-जबल के नाम।
सलामुन अलैक! मैं उस ईश्वर की तुम्हारे समक्ष प्रशंसा करता हूँ जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। तत्पश्चात, ईश्वर तुम्हें महाप्रतिदान दे और तुम्हारे दिल को धैर्य प्रदान करे, और हमें और तुम्हें (अपनी नेमतों पर) कृतज्ञता-प्रकाशन का सौभाग्य प्रदान करे। सत्य यह है कि हमारे प्राण और हमारे धन और हमारे अपने, सब ईश्वर के शुभ और प्रिय उपहार हैं और उसकी सौंपी हुई अमानतें हैं। ईश्वर ने इससे आनन्दपूर्वक लाभ उठाने और आनन्दित होने का सुअवसर प्रदान किया और उसी ने इसे तुमसे बड़े प्रतिदान के बदले में वापस ले लिया। विशेष कृपा, दया और मार्गदर्शन (की शुभ सूचना) है अगर तुमने प्रतिदान को सामने रखकर धैर्य से काम लिया। अतः धैर्य से काम लो और ऐसा न हो कि तुम्हारी बेचैनी और अधीरता तुम्हारे प्रतिदान को नष्ट कर दे। फिर तुम्हें ग्लानि हो। जान रखो कि कोई मरनेवाला अधीरता और बेचैनी से लौटने का नहीं और न इससे दुख और शोक दूर होता है। जो कुछ घटित होनेवाला होता है वास्तव में वह घटित हो चुका होता है।" (हदीस : अत-तबरानी फ़िल-कबीर वल औसत)
व्याख्या : कहा गया कि बच्चे की मृत्यु से तुम्हें जो गहरा सदमा पहुँचा है इसका ईश्वर तुम्हें बड़ा प्रतिफल दे और तुम्हारे हृदय को धैर्य और शान्ति प्रदान करे।
हमारे पास जो चीज़ें भी हैं हम उनके मालिक नहीं हैं। उनका वास्तविक मालिक तो ईश्वर ही है। वह जब तक चाहता है हमें इसका अवसर प्रदान करता है कि हम उनसे लाभ उठाएँ और उनसे दिल बहलाएँ, और जब उसकी इच्छा होती है वह अपनी चीज़ वापस ले लेता है। लेकिन वापस लेने के बदले में उसके यहाँ हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यह उसका महान अनुग्रह और अनुकम्पा है कि "लेता है अपनी चीज़ फिर भी मुफ़्त नहीं लेता।"
क़ुरआन में है—
“जो लोग, उस समय जबकि उनपर कोई मुसीबत आती है, कहते हैं : निस्संदेह हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की ओर लौटनेवाले हैं। यही लोग हैं जिनपर उनके प्रभु की ओर से विशेष कृपाएँ हैं और दयालुता भी; और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर हैं।" (2: 156-57)
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की दी हुई इसी शुभ सूचना की रौशनी में अपने शोकपत्र में ये शब्द लिखवाए कि “विशेष कृपा और दया और मार्गदर्शन की शुभ सूचना है अगर तुमने प्रतिफल और प्रतिदान को दृष्टि में रखते हुए धैर्य से काम लिया।"
धैर्य, प्रतिशोध में
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन बातों का सम्बन्ध ईमान की नैतिकता से है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो अपने क्रोध के प्रभाववश असत्य में न जा पड़े, और जब हर्षित हो तो उसका हर्ष उसे सत्य से विलग न कर दे और जब उसे सामर्थ्य और सत्ता प्राप्त हो तो वह वस्तु न ले जिसे लेने का उसे कोई हक़ न हो।" (हदीस : अल-मोजमुस्सग़ीर लित-तबरानी)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि ईमान को एक विशेष प्रकार की नैतिकता और चरित्र अभीष्ट है। वे तीनों बातें, जिनका इस हदीस में उल्लेख है, वास्तव में ईमान की मौलिक अनिवार्यताओं में से हैं। उनके बिना ईमान अपने मूल तत्व से वंचित ही रहता है।
क्रोध आने पर साधारणतः लोग फ़ौरन ही प्रतिशोध लेने पर आमादा हो जाते हैं और इस मामले में उन्हें उचित-अनुचित का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ईमानी नैतिकता यह है कि क्रोधाग्नि की चरम अवस्था में भी आदमी कोई ऐसा क़दम न उठाए जो सत्य और न्याय के प्रतिकूल हो।
प्रसन्नता की हालत में भी साधारणतया आदमी सीमाओं का उल्लंघन कर बैठता है। वह यह नहीं समझता कि ईश्वर उसे देख रहा है। इसलिए सुख हो या दुख उसके लिए कोई ऐसा व्यवहार अपनाना कदापि शोभा नहीं देता जो सत्य और न्याय के विरुद्ध हो।
दुनिया में शक्ति और सत्ता पाकर भी आदमी भटक जाता है। सत्ता का नशा आसानी से उसे उद्दण्ड बना देता है। जिस चीज़ पर चाहता है अपना अधिकार जमा लेता है। शक्ति और सत्ता किसी को इसलिए नहीं प्रदान की जाती कि वह अपहरण करे। आदमी प्रत्येक दशा में सत्य और न्याय पर क़ायम रहे, ईमान वास्तव में इसी वस्तु का नाम है। इसके बिना हमारा ईमान निरर्थक और निष्प्राण होकर रह जाता है।
धैर्य, शत्रु के मुक़ाबले में
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अबी औफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन दिनों में जिनमें शत्रुओं से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुठभेड़ हुई थी, प्रतीक्षा की यहाँ तक कि सूर्य ढल गया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों के बीच खड़े हुए और उन्हें सम्बोधित किया—
"ऐ लोगो! दुश्मन से मुठभेड़ होने की कामना न करो, और ईश्वर से कुशल-क्षेम चाहो। फिर जब उनसे मुठभेड़ हो ही जाए तो अडिग रहो और जान लो कि जन्नत तलवारों की छाया में है।" फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने खड़े होकर कहा, "ऐ अल्लाह! किताब नाज़िल करनेवाले, बादल को चलानेवाले और जत्थों को भगानेवाले, उन्हें भगा दे और उनके मुक़ाबले में हमारा सहायक हो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस्लाम में युद्ध अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं कि आदमी दुश्मनों से भिड़ने की अभिलाषा करे। अमन-चैन बड़ी नेमत है। उसे नेमत ही समझे और ईश्वर से अमन-चैन का इच्छुक हो। लेकिन अगर सत्य-द्रोहियों को मिटाने और असत्य के ध्वजावाहकों को पराजित करने के लिए मुक़ाबले पर आ जाएँ तो फिर रणभूमि में पीठ दिखाना ईमान के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में दुश्मन से डटकर मुक़ाबला करना चाहिए। दुश्मन के मुक़ाबले में धैर्य से काम लेना और अडिग रहना मोमिन की नीति होती है।
धैर्य, आज्ञापालन में
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"नरक आग की वासनाओं एवं पाश्विक इच्छाओं से ढाँकी गई है। और स्वर्ग (जन्नत) उन चीज़ों से ढाँकी गई है जो मन को अप्रिय होती हैं।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : वासनाओं और मन की तुच्छ इच्छाओं का पालन ही इनसान को नरक में ले जाता है। पाश्विक इच्छाओं के वशीभूत होकर मानव अपना विवेक खो देता है और उसके लिए सत्य और असत्य में अन्तर शेष नहीं रहता। फिर उसे वैध और अवैध की क्या परवाह हो सकती है। उसकी यह नीति उसे नरकीय यातनाओं का भागी बना देती है।
जन्नत पाश्विक इच्छाओं और भोग-विलास का त्याग चाहती है। इस त्याग के बिना मानव में उत्तम चरित्र का विकास सम्भव नहीं। जीवन में ऐसे कितने ही अवसर आते हैं कि इच्छाएँ हमें ऐसी चीज़ों की ओर प्रेरित करती हैं जो नैतिकता और चरित्र के लिए घातक होती हैं। अपनी उच्च नैतिकता और चरित्र के कारण ही आदमी जन्नत का अधिकारी होता है।
मुस्लिम की हदीस में ‘हुजिबत’ के स्थान पर ‘हुफ्फ़त’ शब्द आया है अर्थात जन्नत को उन चीज़ों ने घेर रखा है जो मन को अप्रिय होती हैं और नरक को ऐसी चीज़ों ने घेर रखा है जो मन को आकर्षित करती हैं।
इससे यह भी ज्ञात हुआ कि यह जो कहा गया है कि ‘अल-इल्मु हिजाबुल्लाह’ (ज्ञान ईश्वर और बन्दे के बीच आवरण है) इसका यह अर्थ होता है कि ज्ञान ही हमें ईश्वर तक पहुँचाता है। जिस प्रकार आदमी और उसकी जन्नत के बीच ‘मकारिह’ (परिश्रम और कठिनाइयों) का आवरण है। जो मकारिह को सहन करता है अर्थात पाश्विक इच्छाओं की परवाह किए बिना परिश्रम करता और कठिनाइयाँ झेलता है वह जन्नत को पा लेता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात कर लेता है उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है।
न्याय
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“न्यायकर्ता ईश्वर के यहाँ प्रकाश के मंचों पर प्रतापवान रहमान के दाईं ओर होंगे और उसके दोनों ही हाथ दाहिने हाथ हैं। वे न्यायकर्ता जो अपने आदेशों, अपने लोगों और अपने शासन-क्षेत्र में न्याय करते हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : कृपाशील ईश्वर के दाईं ओर होने का अर्थ यह है कि वे अत्यन्त उच्च और श्रेष्ठ स्थान पर होंगे। वे ऐसे होंगे कि लोग उनका स्थान पाने के अभिलाषी होंगे। दुनिया में वे अन्धकार के बजाय प्रकाश में थे। ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रकाश से वंचित रहकर उन्होंने जीवन व्यतीत नहीं किया था। आख़िरत में भी उन्हें यथोचित बदला मिलेगा। वे प्रकाश के मंचों पर होंगे और उन्हें ईश्वर का सामीप्य प्राप्त होगा। दुनिया में ईश्वरीय मार्गदर्शन का वर्णन क़ुरआन में इस प्रकार हुआ है—
“क्या वह व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर उसे हमने जीवित किया और उसके लिए एक प्रकाश उपलब्ध किया जिसको लिए हुए वह लोगों के मध्य चलता-फिरता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अन्धेरों में पड़ा हुआ हो और उनसे कदापि निकलनेवाला न हो?" (6:122)
भ्रम निवारण के लिए कहा गया कि ईश्वर के दोनों हाथ दाहिने हैं ताकि कोई व्यक्ति यह न समझ बैठे कि जिस प्रकार हमारा बायाँ हाथ दाहिने हाथ की तुलना में कमज़ोर होता है वही हालत ईश्वर के हाथ की भी होगी। ईश्वर हर प्रकार की कमज़ोरी और दोष से पवित्र है। ईश्वर के हाथों की वास्तविकता क्या है इसका सही ज्ञान ईश्वर ही को है। हमें उसके हाथों का अनुमान अपने हाथों पर कदापि नहीं करना चाहिए। क़ुरआन में है—
“उसकी भाँति कोई वस्तु नहीं।" (42:11)
न्यायकर्ता के आदेश न्याय पर आधारित होते हैं। वे कोई ऐसा आदेश नहीं देते जो न्याय और इनसाफ़ से हटकर हो। मामला अपने परिवार और सगे-सम्बन्धियों का हो या किसी और का, इन्साफ़ का दामन उनके हाथ से नहीं छूटता। वे हर किसी के मामले में न्याय की नीति पर क़ायम रहते हैं। हक़ों की अदायगी में भी वे हमेशा शरीअत का ध्यान रखते हैं। जो ज़िम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई हो सम्भव नहीं कि वे उसके सम्बन्ध में ग़ैरज़िम्मेदार साबित हों और अन्यायपूर्ण नीति अपनाएँ।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अहले-किताब (यहूदी और ईसाई) तौरात को इबरानी भाषा में पढ़ते थे और मुसलमानों के लिए उसका अनुवाद और व्याख्या अरबी में करते थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मालूम हुआ तो आपने कहा—
“तुम अहले-किताब की न पुष्टि करो और न उनको झुठलाओ। कहो हम अल्लाह पर और उसपर ईमान लाए जो कुछ हमारी ओर अवतरित किया गया और जो कुछ तुम्हारी ओर अवतरित किया गया।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : तौरात प्रामाणिक रूप में उपलब्ध न थी, फिर इसके अतिरिक्त अहले-किताब के बारे में यक़ीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वे तौरात का अनुवाद या व्याख्या करने में पूरी ईमानदारी से काम लेते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में, हक़ और न्याय के लिए जो अपेक्षित था, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसी को दृष्टि में रखते हुए मुसलमानों को यह शिक्षा दी कि तुम न अहले-किताब की पुष्टि करो और न उनको झुठलाओ। तुम उनकी प्रस्तुत की हुई किसी बात की पुष्टि या उसके खण्डन की स्थिति में नहीं हो। तुम पुष्टि करो, सम्भव है कि वह ग़लत हो। या खण्डन करो, सम्भव है कि वह सही हो। इसलिए सत्य और न्याय की बात यही होगी कि तुम कहो कि हम ईमान लाए जो कुछ हमारी ओर अवतरित हुआ और जो कुछ तुम्हारी ओर अवतरित हुआ। अर्थात ईश्वर की ओर से जो कुछ होगा चाहे तुम्हारे यहाँ तौरात के रूप में अवतरित हुआ हो या हमारे यहाँ क़ुरआन के रूप में अवतरित किया गया हो, हमारा उसपर ईमान है। हमारा ईमान तो ईश्वर द्वारा अवतरित शिक्षाओं पर है। इसमें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वे शिक्षाएँ कब और कहाँ अवतरित हुईं, लेकिन अगर वे ईश्वर की ओर से नहीं हैं तो हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़ि-ल इलैना कहने का आदेश वास्तव में सूरा अल-बक़रा की इस आयत की रौशनी में दिया—
“कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसपर जो हमारी ओर उतरी और उसपर जो इबराहीम और इसमाईल और इसहाक़ और याक़ूब और उनकी सन्तान की ओर उतरी, और जो मूसा और ईसा को मिली, और जो सभी नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। हम उनके बीच अन्तर नहीं करते और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं।” (2:136)
एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अहले-किताब से दीन की कोई बात मत पूछो, कहीं वे तुम्हें कोई सच्ची बात बताएँ और तुम उसे झुठला दो, या ग़लत बात बताएँ और तुम उसकी पुष्टि कर दो।" (हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, तबरानी, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
एक हदीस में यह शिक्षा भी मिलती है कि अहले-किताब की जिस बात की पुष्टि क़ुरआन से होती हो उसका समर्थन करो और उनकी जो बात क़ुरआन के विरुद्ध हो उसका खण्डन करो और जिस बात के सम्बन्ध में क़ुरआन ख़ामोश हो तुम भी उसके विषय में कुछ न कहो, न उसकी पुष्टि करो और न उसे झुठलाओ। इससे अन्दाज़ा होता है कि किसी भी मामले में न्याय की अपेक्षाओं को दृष्टि में रखना ईमानवालों के लिए कितना ज़रूरी है।
सौम्यता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब किसी व्यक्ति की किसी बुरी बात की ख़बर मिलती तो आप यूँ नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति को क्या हुआ कि वह ऐसा कहता है, बल्कि यूँ कहते कि लोगों का क्या हाल हो गया है कि वे ऐसा और ऐसा कहते हैं। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस व्यक्ति का नाम लेकर तंबीह नहीं करते थे बल्कि सामान्य रूप में नसीहत करते, ताकि उस व्यक्ति की निन्दा भी न हो और वह अपना सुधार कर ले और दूसरे भी सचेत हो जाएँ कि इस बुराई से उन्हें दूर रहना चाहिए। इससे इसका भली-भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके स्वभाव में कितनी सौम्यता पाई जाती थी। सदुपदेश और मार्गदर्शन में वे ऐसा तरीक़ा अपनाते थे जो अत्यन्त शिष्ट और मर्यादित होता था। अशिष्ट और सतही अन्दाज़ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नहीं होता था।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि तुफ़ैल (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके साथी आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल! दौस ने कुफ़्र और इनकार की नीति अपनाई, अतः आप उनके लिए बददुआ करें। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि विनष्ट हुए दौस के लोग। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “ऐ अल्लाह! दौस को मार्गदर्शन प्रदान कर और उनको मेरे पास ला।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि लोगों के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कितने करुणामयी थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह स्वीकार्य न था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क़बीला दौस को शापित करें। शाप देने के बजाए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़बीला दौस के लोगों के लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह! उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर और उन्हें इसका सौभाग्य प्रदान कर कि वे अपने रसूल की ओर पलटें।
(3) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि हमने एक बार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ मग़रिब की नमाज़ अदा की। फिर हमने कहा कि अगर हम बैठे रहें यहाँ तक कि इशा की नमाज़ भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ अदा करें तो अच्छा रहेगा। वे कहते हैं कि हम बैठे रहे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बाहर हमारे पास आए और कहा, "तुम यहाँ बैठे रहे?” हमने कहा कि हमने आप के साथ मग़रिब की नमाज पढ़ी, फिर हमने सोचा कि हम बैठे रहें यहाँ तक कि इशा की नमाज़ भी आप के साथ अदा करें तो अच्छा रहेगा। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— "तुम ने अच्छा किया और ठीक किया।” फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आसमान की तरफ़ अपना सिर उठाया, और आप अकसर आसमान की तरफ़ सिर उठाते, फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “तारे आसमान का बचाव और सुरक्षा हैं। तारे जब मिट जाएँगे तो जिस चीज़ का वादा है वह आसमान पर घटित हो जाएगा। और मैं अपने साथियों (सहाबा) के लिए सुरक्षा और आश्रय हूँ। जब मैं प्रस्थान कर चुकूँगा तो मेरे साथियों पर वह समय भी आ जाएगा जिसका वादा है। और मेरे साथी मेरी उम्मत के लिए बचाव और सुरक्षा की हैसियत रखते हैं। जब मेरे साथी दुनिया से प्रस्थान कर चुके होंगे तो मेरी उम्मत पर वह समय आ जाएगा जिसका वादा है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : 'आसमान पर घटित हो जाएगा' अर्थात् आसमान चाक हो जाएगा। ब्रह्मांड की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी और क़ियामत घटित हो जाएगी।
कहा गया कि मेरी उपस्थिति सहाबा के लिए सुरक्षा-प्राचीर की भाँति है। मेरी उपस्थिति में कोई उपद्रव सिर नहीं उठा सकता और न गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मेरे बाद यह स्थिति शेष न रहेगी। मेरे सहाबा को मेरे बाद बिगाड़ और उपद्रवों का सामना करना पड़ेगा।
सहाबा के बाद इसकी सम्भावना है कि बिदअतें प्रकट हों अर्थात दीन के नाम से बहुत-सी ऐसी चीज़ें अपनाई जाने लगें जिनका दीन से कोई सम्बन्ध न हो। दृष्टिकोण में परिवर्तन आए और दीन की सही अवधारणा दृष्टि से ओझल हो जाए और इस्लाम स्वयं अपनों के बीच अपरिचित होकर रह जाए। आपस में घोर मतभेद उत्पन्न हो जाएँ और मुस्लिम समुदाय में अराजकता व्याप्त हो जाए। अज्ञानपूर्ण धारणाओं और विचारधाराओं से वातावरण आच्छादित हो जाए। विरोधी क़ौमें वर्चस्व प्राप्त कर लें और ईमानवालों पर अत्याचारों के पहाड़ तोड़े जाएँ, आदि।
इस हदीस से मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उपस्थिति और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बाद सहाबा की उपस्थिति मानो एक ऐसे क़िले के सदृश है जो प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करता है। हम देखते भी हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी क़ौम के लिए एक बड़ी ताक़त थे। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण सहाबा हर प्रकार के उपद्रवों और बिगाड़ से सुरक्षित रहे। फिर हम यह भी देखते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मृत्यु के बाद सहाबा निष्क्रिय होकर नहीं बैठे रहे बल्कि उन्होंने उम्मत का मार्गदर्शन किया। उनके त्याग से दीन अपने प्रामाणिक और पूर्ण रूप में उम्मत तक पहुँचा। उनका जीवन उम्मत के लिए मार्गदीप सिद्ध हुआ। सहाबा का अस्तित्व दुनिया में कोई बेजान अस्तित्व न था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनमें वह शक्ति और उत्साह भर दिया था कि जिसको ज़माना ख़त्म न कर सका। लेकिन सहाबा के बाद उपद्रव बढ़ता गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि मुसलमानों के लिए अपनी ऊर्जा का यही उपयोग रह गया कि वे उसे परस्पर लड़ने और एक-दूसरे को हानि पहुँचाने में लगा रहे हैं। अब न वह विवेक और अन्तर्दृष्टि दिखाई देती है न वह सौम्यता और सज्जनता और न ही उत्तरदायित्व का वह एहसास कि जिससे कभी युग निर्माण का काम लिया जाता था।
(4) हज़रत आइज़-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अबू-सुफ़ियान सलमान (रज़ियल्लाहु अन्हु), सुहैब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास आया। वहाँ और भी कुछ लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की तलवारें ईश्वर के शत्रु की गर्दन पर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचीं। इसपर अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि क्या तुम ऐसा क़ुरैश के बड़े-बूढ़े और उनके सरदार के सम्बन्ध कहते हो। फिर वे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से यह बात कही। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “ऐ अबू-बक्र! तुमने शायद उन लोगों को क्रुद्ध किया। अगर तुमने उन्हें क्रुद्ध किया तो वास्तव में तुमने अपने प्रभु को क्रुद्ध किया है।" यह सुनकर अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) उनके पास आए और कहने लगे, “ऐ भाइयो! मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया।" वे बोले, “नहीं, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे ऐ हमारे भाई!" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : “क्या ऐसा तुम क़ुरैश के बड़े-बूढ़े और उनके सरदारों के विषय में कहते हो।" हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह बात इसलिए कही थी कि अबू-सुफ़ियान क्रोधित होकर इस्लाम स्वीकार करने की बजाए कहीं हमेशा के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन से वचिंत होकर न रह जाएँ। स्पष्ट रहे कि यह उस समय की बात है जब अबू-सुफ़ियान ईमान नहीं लाए थे। सुल्ह करके मुसलमानों के पास आए थे।
“ऐ अबू-बक्र, तुमने शायद उन लोगों को नाराज़ किया" नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इस बात से जहाँ हज़रत सलमान (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत सुहैब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) की श्रेष्ठता का पता चलता है वहीं यह भी मालूम होता है कि निर्बलों और ईमानवालों का सत्कार और उनका दिल रखने का कितना अधिक महत्व है। हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की यह विशालहृदयता थी कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात से तुम्हें नाराज़ कर दिया। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बात से तुम्हें तकलीफ़ पहुँची होगी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
विनम्रता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सद्क़े से माल में कमी नहीं आती। और ईश्वर किसी बन्दे के क्षमाशील होने पर उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए विनम्रता अपनाता है तो ईश्वर उसे अनिवार्यतः उच्च कर देता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : आम तौर पर लोग समझते हैं कि सद्क़ा करने से उनके माल में कमी आ जाएगी। इसी तरह आम तौर पर लोग यह भी सोचते हैं कि अगर हम क्षमा से काम लेंगे और लोगों के साथ नर्मी का व्यवहार करेंगे तो वे इसे हमारी कमज़ोरी और मजबूरी समझेंगे। विनम्रता के बारे में यह ग़लतफ़हमी पाई जाती है कि यह सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। इस हदीस में लोगों की ग़लतफ़हमियों और उनकी निर्मूल शंकाओं को दूर किया गया है और बताया गया है कि सद्क़े से माल में कमी नहीं आती। वास्तविकता यह है कि सद्क़ा देकर बन्दा ईश्वर के शुक्रगुज़ार बन्दों में शामिल होता है। ईश्वर अपने शुक्रगुज़ार बन्दों को अपने अतिरिक्त अनुग्रह से सम्मानित करता है जैसा कि उसका वादा है—
“अगर तुम शुक्रगुज़ार हुए तो मैं तुम्हें और अधिक दूँगा।" (12:7)
इसी तरह क्षमाशीलता से काम लेने के लिए विशालहृदय होना आवश्यक है। यह किसी छोटे आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। इसलिए यह ग़लतफ़हमी न हो कि क्षमाशीलता और नर्मी से काम लेंगे तो इससे अपनी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचेगा। क्षमा से प्रतिष्ठा में कमी नहीं, वृद्धि होती है।
ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति विनम्रता अपनाता है तो ईश्वर उस का दर्जा उच्च कर देता है। विनयशीलता मानव के नैतिक अस्तित्व का सौन्दर्य है। सौन्दर्य जहाँ कहीं पाया जाएगा वह स्वयं लोगों से अपना महत्व स्वीकार करा लेगा।
(2) हज़रत अयाज़-बिन-हिमार मुजाशिई से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने मेरी ओर प्रकाशना की कि विनम्रता अपनाओ, यहाँ तक कि न कोई व्यक्ति किसी की प्रतिस्पर्धा में गर्व करे और न कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अत्याचार करे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : गर्व और बड़प्पन साधारणतया अत्याचार और सीमोल्लंघन का कारण बनता है, इसी लिए दोनों का उल्लेख एक साथ किया गया कि न तो कोई किसी व्यक्ति के मुक़ाबले में गर्व करे और न कोई किसी के मुक़ाबले में अत्याचार और सीमाओं का उल्लंघन करे।
ऐसा व्यक्ति किसी घमण्ड में नहीं पड़ता। विनम्रता उसका स्वभाव होती है। ईश्वर को यह बात प्रिय होती है और वह उसे उच्चता प्रदान कर देता है। इसका एक प्रभाव दुनिया में यह प्रकट होता है कि लोगों की दृष्टि में उसे महानता प्राप्त हो जाती है और लोग उसका सम्मान करने लगते हैं।
(3) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। उन्होंने मिम्बर पर कहा कि लोगो! विनयशीलता अपनाओ, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते सुना है कि जो व्यक्ति ईश्वर के लिए विनम्रता अपनाए, ईश्वर उसे उच्चता प्रदान कर देता है। वह अपने आपको छोटा समझता है लेकिन लोगों की दृष्टि में बड़ा होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति गर्व और घमण्ड करता है, ईश्वर उसे हीन कर देता है। फिर वह लोगों की दृष्टि में छोटा और तुच्छ होता है जबकि वह स्वयं को बड़ा समझता है। यहाँ तक कि उसकी यह हालत हो जाती है कि वह लोगों की दृष्टि में कुत्ते और सूअर से भी हीन हो जाता है। (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : घमण्डी व्यक्ति तो अपनी दृष्टि में स्वयं को सबसे ऊँचा समझता है लेकिन ईश्वर उसे हीन और अपमानित कर देता है। इसका परिणाम दुनिया में भी प्रकट होकर रहता है। वह लोगों की दृष्टि में अधम और क्षुद्र होता है। यह अपमान इस सीमा तक बढ़ सकता है कि लोग उसे कुत्ते और सूअर से भी गिरा हुआ समझने लगें। कुत्ते और सूअर तो जन्मजात क्षुद्र होते हैं और वह नैतिक रूप से क्षुद्र होता है। यह अधमता और गिरावट की अन्तिम सीमा है।
सादगी
(1) हज़रत अबू-उमामा-बिन-सअ्लबा अनसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने दुनिया की चर्चा की। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “क्या तुम सुनते नहीं! क्या तुम सुनते नहीं कि सादा ढंग से रहना ईमान के स्वभाव में से है, सादा ढंग से रहना ईमान के स्वभाव में से है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : "क्या तुम सुनते नहीं! क्या तुम सुनते नहीं!" ऐसा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसलिए कहा ताकि लोग पूर्णतः ध्यान देकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बात सुनें और यह समझकर सुनें कि जो बात कही जा रही है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है।
इस हदीस में जिस शब्द का अनुवाद यहाँ 'सादा ढंग से रहना' किया गया है वह अल-बज़ाज़ा है जो पुरानेपन, फटेहाली आदि के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ इससे अभिप्राय वह जीवन है जो असहजता और कृत्रिमता से सर्वथा पवित्र हो। गर्व, दिखावा और भोग-विलास को इस्लाम पसन्द नहीं करता। सुरुचि इस्लाम में वर्जित नहीं, अलबत्ता यह चीज़ अगर दीवानगी तक पहुँच जाए तो यह ईमान के विरुद्ध होगी।
भोग-विलास का मतलब यह होता है कि आदमी का सारा ध्यान और दिलचस्पी संसार की ऊपरी साज-सज्जा और विलासिता से सम्बद्ध होकर रह जाए। न उसे आनेवाले कठिन दिन की चिन्ता हो और न ही आख़िरत में प्राप्त होनेवाले आनन्दमय जीवन की प्रतीक्षा ही उसमें पाई जाए। निगाह और समझ की कमी के कारण वह सतही जीवन का अनुरागी होकर रह जाए। स्पष्ट है कि यह चीज़ कभी इस्लाम की दृष्टि में प्रिय नहीं होती।
इस्लाम में जिस तथ्य को उद्घाटित किया गया है वह यह है कि जीवन अभी परिपूर्ण नहीं है और इसकी परिपूर्णता से पहले किसी व्यक्ति का इस प्रकार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना मानो यह सांसारिक भोग-विलास ही सब कुछ है, जो इससे चूक गया वह अत्यन्त घाटे में रहेगा। यह विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस्लाम से मेल नहीं खाता। एक दूसरी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने अच्छा और क़ीमती वस्त्र पहनना त्याग दिया हालाँकि उसे इसकी क्षमता प्राप्त थी कि वह क़ीमती और अच्छा वस्त्र धारण कर सके —उल्लेखकर्ता कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह भी कहा कि उसने ऐसा सादा स्वभाव के कारण किया— तो अल्लाह उसे (परलोक में) सम्मान का वस्त्र पहनाएगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)
इस हदीस से ज्ञात होता है कि मोमिन को सादगी और विनम्रता के स्वभाव की रक्षा करनी चाहिए और इसे अपने अन्दर उसको विकसित करने की चिन्ता होनी चाहिए। हमारे बाह्य स्वभाव एवं व्यवहार से एक ओर हमारा अन्तर प्रतिबिम्बित होता है तो दूसरी ओर हमारा अन्तर हमारे बाह्य स्वभाव से प्रभावित होता है। इसलिए वस्त्र धारण करने के मामले में ही नहीं बल्कि हर मामले में हमें उस जीवन शैली को ही प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे एक मोमिन के जज़्बे और स्वभाव को ठेस न पहुँचे।
प्रसन्नता और ख़ुशमिज़ाजी
(1) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी भी नेकी को तुच्छ न समझो, चाहे वह तुम्हारा अपने भाई से प्रसन्न मुद्रा के साथ मिलना ही क्यों न हो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात कोई भी नेकी चाहे वह देखने में साधारण ही क्यों न हो, छोटी और तुच्छ नहीं होती। यहाँ तक कि प्रसन्नतापूर्वक अपने भाई से मिलने को भी साधारण बात नहीं समझना चाहिए। यहाँ भाई से अभिप्रेत सारे इनसान हैं। क्योंकि इनसान आपस में भाई-भाई हैं। नेकी अगर नेकी है तो वह मूल्यवान है। उसे तुच्छ समझना सही नहीं। इसलिए कि उसका सम्बन्ध उस विचार और सुरुचि से होता है जो जीवन की अत्यन्त बहुमूल्य निधि है। मोमिन के छोटे-से-छोटे कर्मों से भी उसके ईमान और उस सम्बन्ध का पता चलता है जो उसके और ईश्वर के बीच पाया जाता है। छोटा कर्म भी, अगर उसका सम्बन्ध जीवन की सच्चाइयों और मौलिक मान्यताओं से है, तो वह छोटा कर्म कदापि नहीं है। इसके विपरीत बड़े-से-बड़े कार्य का भी ईश्वर की दृष्टि में कोई वज़न नहीं हो सकता अगर उसके पीछे सही सोच और ईश-प्रसन्नता की भावना कार्यरत न हो।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि सहाबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमसे विनोदपूर्ण बातें करते हैं? रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं केवल सत्य कहता हूँ।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात मैं विनोदपूर्वक जो बातें कहता हूँ वे सत्य के विरुद्ध कदापि नहीं होतीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शुष्क स्वभाव के नहीं थे। आप के विनोद में सूक्ष्मता पाई जाती थी। इसका उद्देश्य आत्मीयता लाना और सम्बोधित व्यक्ति को प्रसन्न करना होता था।
हास्य-विनोद उसी सीमा तक उचित है जिससे किसी को दुख न पहुँचे। इसके अतिरिक्त किसी के लिए हास्य को अपना ऐसी दिनचर्या बनाना उचित नहीं कि उसकी अधिकता से आदमी की अपनी गरिमा को आघात पहुँचे या ईश्वर के स्मरण और आख़िरत की चिन्ता से उसके ग़ाफ़िल हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाए।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक बूढ़ी स्त्री से कहा कि “बूढ़ी औरत जन्नत में दाख़िल न होगी।" उसने कहा कि क्या कारण है कि ऐसी औरतें जन्नत में न जा सकेंगी? वह स्त्री क़ुरआन पढ़ी हुई थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “क्या तुमने क़ुरआन में यह नहीं पढ़ा कि निश्चय ही उन (जन्नती) औरतों को एक विशेष उठान पर उठाया और हमने उन्हें कुँवारियाँ बनाया।” (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : 'बूढ़ी स्त्री जन्नत में प्रवेश न करेगी' यह बात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विनोद भाव से कही। इसको सुनकर बूढ़ी महिला घबरा जाती है और कहती है कि आख़िर बूढ़ी स्त्रियों का क्या दोष है कि वे दूसरी मोमिन स्त्रियों के साथ जन्नत में प्रवेश न कर सकेंगी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनकी हैरानी, परेशानी और दुख को जल्दी ही दूर कर देते हैं कि मैंने जो बात कही है वह तो क़ुरआन के बयान के अनुसार कही है। क्या क़ुरआन में ये आयतें नहीं हैं जिनसे मालूम होता है कि ईश्वर औरतों को वृद्धावस्था में नहीं बल्कि कौमार्य की दशा में जन्नत में प्रवेश कराएगा। कोई स्त्री जन्नत में बूढ़ी न होगी। वहाँ जो स्त्रियाँ भी होंगी वे नवयौवना, सुन्दर और प्रेयसी होंगी। क़ुरआन में कहा गया है—
“और निश्चय ही हमने उन औरतों को एक विशेष उठान पर उठाया और हमने उन्हें कुँवारियाँ बनाया, प्रेम दर्शानेवाली और समायु, सौभाग्यशाली लोगों के लिए।" (56: 35-38)
दानशीलता
(1) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या तुम जानते हो कि दानशीलों में कौन सबसे बढ़कर दानशील है?” सहाबियों न कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “दानशीलों में अल्लाह सबसे बढ़कर दानशील है, फिर आदम की सन्तान में सबसे ज़्यादा दानशील मैं हूँ और मेरे बाद लोगों में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा दानशील है जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रसार किया। वह क़ियामत के दिन एक अमीर की हैसियत से आएगा।" या कदाचित यह कहा, "वह इस हाल में उपस्थित होगा कि वह अपने आप में एक उम्मत (समुदाय) होगा।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : इस हदीस से केवल यही नहीं कि दानशीलता और उदारता के महत्व का पता चलता है बल्कि यह भी मालूम होता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है। दुनिया में सबसे बहुमूल्य वस्तु ज्ञान है। यहाँ ज्ञान से अभिप्रेत दीन का ज्ञान है। क़ुरआन में विभिन्न स्थानों पर बताया गया है कि नबियों को तत्वज्ञान और अन्तर्दृष्टि प्रदान की गई थी। नुबूवत को भी कितने ही स्थानों पर ज्ञान और हिकमत (तत्वज्ञान) से अभिव्यंजित किया गया है। ज्ञान ही के कारण मानव को दूसरे प्राणियों के मुक़ाबले में श्रेष्ठता और महानता प्राप्त है।
ज्ञान की वास्तविक प्राप्ति वही है जिसके बाद आदमी के व्यावहारिक जीवन में वह ज्ञान प्रकट हो सके। ज्ञान और हिक्मत एक प्रकाश है। प्रकाश जहाँ कहीं पहुँचता है उसे प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार जब आदमी को सही तौर पर ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल यही नहीं कि उसका अन्तर्मन प्रकाशमान हो उठता है बल्कि उसके जीवन से भी अन्धकार के बादल छट जाते हैं।
क्या यह सम्भव है कि कोई भूखा भी हो और उसे स्वच्छ और पवित्र भोजन उपलब्ध हो और वह सिर्फ़ उसका नाम लेकर रह जाए और उसे ग्रहण न करे। लेकिन कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जो देखने में ज्ञान से भरे हैं किन्तु उनके जीवन से उनके ज्ञान का प्रमाण नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सत्य को जानना चाहिए उस प्रकार उन्होंने सत्य को नहीं जाना। जानने का अर्थ तो यह है कि आदमी का ज्ञान उसके लिए प्रेरणा शक्ति बन जाए और उसे कर्म पर उभार सके। इस प्रकार का ज्ञान आदमी के लिए मात्र एक सूचना बनकर नहीं रहता, बल्कि वह तो हृदय के कोमल तारों को झंकृत करता है और आदमी उत्कृष्ट भावनाओं और भावों से समृद्ध हो जाता है वह उसे एक पवित्र संसार से केवल परिचित ही नहीं कराता बल्कि उसमें उसे प्रविष्ट करा देता है जिससे प्रस्थान उसके लिए सम्भव नहीं रहता। उसे मन-मस्तिष्क का वह पवित्र वातावरण उपलब्ध होता है जहाँ न तो कोई उपद्रव पाया जाता है और न कोई अन्तर्विरोध। जहाँ किसी प्रकार की कोई संकीर्णता नहीं होती। आदमी स्वयं को ईश्वर से सीधे लाभान्वित होता हुआ महसूस करने लगता है।
ईश्वर की हस्ती महान और बरकतवाली है। कौन-सी ऐसी नेमत है जो उसने इनसानों को प्रदान नहीं की। स्वयं हमारा अपना अस्तित्व उसकी अनुकम्पा का जीवित प्रमाण है। फिर उसने हमारे लिए जीवन के समस्त साधन उपलब्ध किए हैं। क़ुरआन में है—
“वही तो है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो धरती में है।" (2:29)
“क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने, जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है, सबको तुम्हारे काम में लगा रखा है और उसने तुमपर अपनी प्रकट और अप्रकट अनुकम्पाएँ पूर्ण कर दीं।” (31:20)
ईश्वर के बाद उसके बन्दों में सबसे बढ़कर दानशील उसका रसूल होता है जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुँचते हैं। रसूल केवल हमें ईश्वर का अन्तर्बोध ही प्रदान नहीं करता बल्कि उस प्रेम-भाव से, जो अल्लाह को प्रिय है, वह स्वयं सबसे बढ़कर सुशोभित होता है। कोई व्यक्ति ईश्वर को जितना अधिक पहचानता होगा स्वाभाविक रूप से वह उतना ही दानशील होगा। रसूल सबसे ज़्यादा ईश्वर को जानते और पहचानते हैं। अल्लाह के रसूल ने स्वयं कहा है—
"तुममें सबसे ज़्यादा डर रखनेवाला और तुम सबसे बढ़कर ईश्वर को जाननेवाला मैं हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
नबी के बाद सबसे बढ़कर दानशील वह व्यक्ति ठहरता है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास में लग जाता है और ज्ञान का प्रसार करता है। इसलिए कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई दौलत नहीं पाई जाती। वह ज्ञान का प्रसार करता और ईश्वर के बन्दों को ईश्वरीय मार्गदर्शन की ओर बुलाता है। उनके कल्याण और सफलता की सामग्री जुटाता है। ऐसा व्यक्ति दानशील ही नहीं एक नेता और पथप्रदर्शक भी होता है। यही कारण है कि क़ियामत के दिन वह एक नायक और नेतृत्त्वकर्त्ता की शान के साथ ईश्वर के सामने उपस्थित होगा। उसका यह महत्व व्यक्तिमात्र का महत्व न होगा, बल्कि वह अपने आप में एक उम्मत (समुदाय) की हैसियत रखता होगा। क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ़ अपनी ही चिन्ता न थी बल्कि वह सम्पूर्ण मानवता के लिए चिन्तित और व्याकुल रहा और उससे एक बड़े जनसमुदाय ने लाभ उठाया।
(2) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह उस व्यक्ति पर रहम करे जो दानशील है, जब वह बेचे, जब वह ख़रीदे और जब वह अपना हक़ माँगे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्यख्या : अर्थात उसकी दानशीलता विभिन्न अवसरों और विभिन्न मामलों में प्रकट होती है। वह अपना ही नहीं अपने ग्राहक का भी शुभचिन्तक होता है। तौलकर देता है तो तौलते समय तराज़ू का (देनेवाला) पलड़ा झुका रखता है। वह कम नहीं तौलता। अगर किसी से कुछ ख़रीदता है तो उसका यह प्रयास हरगिज़ नहीं होता कि वह उचित-अनुचित हर प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा माल समेट ले। इसी प्रकार जब वह किसी से अपना अधिकार तलब करता है तो नर्मी से काम लेता और अधिक-से-अधिक मोहलत देता है, बल्कि अगर आवश्यकता पड़े तो वह क्षमा से काम लेते हुए अपना अधिकार छोड़ भी सकता है। उसका यह व्यवहार उसकी विशाल-हृदयता और उदारता का स्पष्ट प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के क्रोध का नहीं बल्कि उसकी अनुकम्पा का हक़दार होता है। ईश्वर अनिवार्यतः उसपर दया करेगा। अगर हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आशीर्वचनों के अनुरूप बनना चाहते हैं (और कौन मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ न लेना चाहेगा) तो हमें चाहिए कि हम हर प्रकार की कृपणता और तंगदिली से बचें और उदारता को अपना स्वभाव बनाएँ।
(3) हज़रत मालिक-बिन-नज़ला (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
"हाथ तीन प्रकार के हैं। एक हाथ तो ईश्वर का है जो सर्वोच्च है, एक देनेवाले का हाथ है जो उसके निकट है और एक माँगने वाले का हाथ है जो नीचे होता है। अतः जो आवश्यकता से अधिक हो दो और अपनी इच्छाओं के अधीन न हो।”
व्याख्या : इस हदीस में उदारता और दानशीलता के महत्व को इस प्रकार उजागर किया गया है जिससे मनुष्य में उसके लिए असीम अभिलाषा उत्पन्न हो सके। सबसे अच्छा हाथ ईश्वर ही का हो सकता है। कहा गया कि ईश्वर का हाथ सर्वोच्च है अर्थात उसका हाथ माँगनेवाला नहीं, देने वाला है।
"ऊँचा हाथ वह है जो ख़र्च करता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
ईश्वर की उदारता और दानशीलता असीमित है। जो कुछ देता है किसी से लेकर नहीं, अपने पास से देता है। वह अपने शत्रुओं को भी आजीविका से वंचित नहीं रखता। बदले में बन्दों से आजीविका नहीं माँगता है।
“वही तो है जो खिलाता है, ख़ुद नहीं खाता।” (6:1-4)
वह मात्र पेट ही नहीं भरता, हृदय और आत्मा के लिए भी आहार जुटाता है। फिर वह आजीविका प्रदान करने के इस क्रम को बन्द भी नहीं करना चाहता। यह अलग बात है कि कोई शिर्क और कुफ़्र पर जान देकर स्वयं ही अपने को ईश्वर के उपहारों से वंचित कर ले।
ईश्वर के बाद ऊँचा हाथ उस व्यक्ति का है जो ख़र्च करता है, जिस के दिल को लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने से आराम मिलता है।
इसके बाद तो बस माँगनेवाले का हाथ रह जाता है, जो लोगों के आगे हाथ फैलाता और उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निवेदन करता फिरता है। यह हाथ ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। इसलिए अगर अल्लाह ने किसी को आवश्यकता से अधिक दिया है तो उसे ईश्वरीय मार्ग में ख़र्च करना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा के अनुसरण से बचना चाहिए। इच्छाएँ तो आम तौर पर आदमी को लोभ और कृपणता ही पर उभारती हैं। ईश्वर से दूरी कोई स्थानगत दूरी नहीं। ईश्वर तो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। उसका सामीप्य प्राप्त करने के लिए समय और स्थान की दूरी तय नहीं करनी पड़ती। नैतिक गुण ही उससे निकटता प्राप्त करने में हमारे सहायक होते हैं।
(4) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक-दूसरे पर दया न करो।” सहाबियों ने कहा कि हममें से प्रत्येक दयाशील है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "मेरा आशय यह नहीं है कि तुममें से कोई अपने साथी पर दया करे बल्कि मेरा अभिप्राय सार्वजनिक दयालुता से है।" (हदीस : अत-तबरानी)
व्याख्या : मालूम हुआ कि यह ईमान का तक़ाज़ा है कि आदमी साहसी हो और हर प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण और कृपणता से मुक्त हो। वह केवल अपने ही लोगों पर दया न दर्शाए बल्कि उसकी दयालुता सबके लिए हो। वह सारे ही इनसानों का हमदर्द और उनका शुभचिन्तक बनकर रहे। एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“समस्त जन ईश्वर का कुटुम्ब हैं। अतः ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय वह व्यक्ति है जो उसके कुटुम्ब के साथ सद्व्यवहार करे।" (हदीस : बैहक़ी)
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “दानशील ईश्वर से निकट है, लोगों से निकट है और स्वर्ग से निकट है और नरक से दूर है। इसके विपरीत कृपण ईश्वर से दूर है, लोगों से दूर है और स्वर्ग से दूर है और नरक से निकट है और निस्सन्देह एक दानशील व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में इबादत करनेवाले कृपण से बढ़कर प्रिय होता है यद्यपि वह विद्वान न हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात दानशील और उदार व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न होता है और उसे अपना निकटवर्ती बना लेता है और लोग भी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते और उसे अपना समझते हैं। जिस व्यक्ति से ईश्वर और उसके बन्दे सभी प्रसन्न हों उसके स्वर्ग के अधिकारी होने में क्या सन्देह हो सकता है। इसके विपरीत कृपण व्यक्ति से न ईश्वर प्रसन्न होता है और न लोगों को उससे लगाव हो सकता है। उसका परिणाम नरक के सिवा और क्या होगा।
नैतिकता एक सौन्दर्यबोध बनकर मानव जीवन में सन्निहित रहती है। जो व्यक्ति इस सौन्दर्य से आनन्दित और उसके महत्व और मूल्य से परिचित न हो उसका स्वर्ग से कैसे कोई सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। स्वर्ग वास्तव में समस्त गुणों और नेमतों की सम्पूर्णता का नाम है। इसके विपरीत प्रत्येक प्रकार की विकृतियों और गन्दगियों की सम्पूर्णता का दूसरा नाम नरक है। विकारों और गन्दगियों को इख़्तियार करने का अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं कि इस प्रकार एक बुरा व्यक्ति अपने नारकीय होने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। अब अगर वह इससे बाज़ नहीं आता तो उसे कोई चीज़ नरक से नहीं बचा सकती। उसका अस्तित्व तो सही अर्थों में स्वयं नरक का एक अंग होता है। वह नरक से कैसे दूर रह सकता है।
दानशीलता इस बात का लक्षण है कि उसके जीवन और सत्य में एक आत्मीयता पाई जाती है। यद्यपि सामान्य अर्थों में वह कोई बड़ा ज्ञानवान और इबादतगुज़ार व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत कृपण व्यक्ति की कृपणता उसके समस्त गुणों पर पानी फेर देती है। कृपण व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित होता है। उसके जीवन में प्रेरक तत्व साधारणतः भौतिक लाभ ही होता है। देखने में वह नमाज़ें पढ़ता और ईश्वर का नमन करता है। ऐसी स्थिति में उसका वह स्थान कैसे हो सकता है जो एक दानशील व्यक्ति का होता है।
भलाई के कामों में ख़र्च करना
(1) हज़रत असमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (मुझसे) कहा—
“भलाई के कामों में ख़र्च करो, गिनो मत, अन्यथा ईश्वर तुम्हें भी गिनकर देगा। और रोको मत अन्यथा ईश्वर भी तुमसे रोकेगा, और दो जितना दे सकती हो।” (बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से दान के महत्व का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। एक हदीस क़ुदसी में है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि अल्लाह कहता है—
“ऐ आदम के बेटे! (भलाई के कामों में) ख़र्च कर, तुझ पर ख़र्च किया जाएगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
दानशीलता को धर्म में मौलिक महत्व प्राप्त है। इसके कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो कई तथ्यों का उद्घाटन होता है। दानशीलता का सम्बन्ध सीधे ईश्वरीय गुण से है। अगर हमारे प्रभु में यह गुण न होता तो दुनिया में यह जो कुछ आपको नज़र आता है कुछ भी नज़र नहीं आ सकता था। यह उसका कृपादान है जो हमें अपने अस्तित्व और इस विस्तृत संसार के रूप में दिखाई दे रहा है।
दानशीलता एक वैश्विक नियम (Universal and Cosmic Law) का महत्व रखती है। अगर एक क्षण के लिए भी इस नियम में गतिरोध उत्पन्न कर दिया जाए तो यह जगत् स्वतः ही विनष्ट हो जाए। इस संसार की व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार हुई है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बल मिलता है। सूर्य अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और ताप को निरन्तर व्यय करता है जिसके परिणामस्वरूप इस धरती पर जीवन सम्भव हो सका है। हमारी कितनी ही आवश्यकताएँ इसपर निर्भर करती हैं कि सूर्य अपनी दानशीलता के क्रम को एक पल के लिए भी न रोके। ऋतु परिवर्तन, फ़सलों का पककर तैयार होना इत्यादि। कौन नहीं जानता कि यह सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि सूर्य अपनी ऊर्जा और ताप समेटकर न रखे बल्कि दुनिया को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलता रहे।
समुद्र अपना पानी देने में किसी कृपणता से काम नहीं लेता। समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर बादल का रूप लेता है जिसे हवाएँ उड़ाकर लाती हैं। फिर उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाकर धरती को सिंचित करने की व्यवस्था करती हैं जिसके परिणामस्वरूप धरती हरित हो जाती है।
कितने पेड़-पौधे हैं, उनमें हमारे लिए मीठे फल लगते हैं। पशु-जगत् का हाल भी इससे अलग नहीं। गायों के थनों में दूध इसलिए नहीं जमा होता कि वह जमा रहे बल्कि वह ख़र्च होने के लिए ही पैदा होता है। इस दूध को गाय का बच्चा भी पीता है और वह हमारे प्रयोग में भी आता है।
फिर विश्व में कितनी ही अदृश्य शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार सुरक्षित नहीं रखी गईं कि हम उनसे लाभ न उठा सकें। अगर धरती का गुरुत्वाकर्षण धरती के अलावा किसी दूसरे फ़ायदे के लिए न होता तो इस धरती पर जीवन यापन का प्रश्न ही नहीं उठता।
इस प्रकार जिस ओर भी दृष्टि की जाए यह प्रमाण मिलेगा कि सम्पूर्ण विश्व दानशीलता के नियम और क़ानून के सहारे चल रहा है। विश्व का कोई भाग दूसरे भाग से असम्बद्ध नहीं है। मानव के लिए ईश्वर की दयालुता और दानशीलता इतनी बढ़ी हुई है कि उसने केवल हमें बाह्य नेमतें ही प्रदान नहीं कीं बल्कि आन्तरिक नेमत और ज्ञान और तत्वदर्शिता से भी हमें मालामाल किया है। और इसके लिए उसने वह्य (प्रकाशना) और रिसालत का सिलसिला जारी किया। उसकी दानशीलता की कोई सीमा नहीं। यह उसकी दानशीलता ही है जिसे हम आख़िरत से अभिव्यंजित करते हैं। क़ुरआन में कहा गया है—
“अगर तुम अल्लाह की नेमतों की गणना करना चाहो तो उनकी पूरी गणना नहीं कर सकते।" (14:34)
“क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, सबको तुम्हारे काम में लगा रखा है और उसने तुमपर अपनी प्रकट और अप्रकट अनुकम्पाएँ पूर्ण कर दी हैं।" (31:20)
ईश्वर की मानव पर विशेष अनुकम्पा है। वह उसे व्यक्तित्व की उच्चता और चरित्र की महानता से परिपूर्ण देखना चाहता है। वह चाहता है कि हमारा बाह्य व्यक्तित्व भी अर्थपूर्ण और प्रतिष्ठित हो। लेकिन कितनी ही चीज़ें हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। ईश्वर की असीम अनुकम्पाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक है कि हम विशाल-हृदय हों। हमारे व्यक्तित्व ऐसे हों कि वे ईश्वर के विशेष अनुग्रहों को धारण कर सकें।
यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि विशाल-हृदयता, श्रेष्ठ योग्यता और प्रतिभा की प्राप्ति के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? इसका एक ही सही जवाब है कि आदमी धर्म में सोच-विचार और समझ प्राप्त करे और धर्म के निर्देशों का पालन करे। धर्म का वास्तविक उद्देश्य ही यह है कि मानव का आत्मविकास हो और उसकी आत्मा भी विकसित हो और वह प्रत्येक प्रकार की अधमता और संकीर्णता से मुक्त हो। क़ुरआन में है—
“जो व्यक्ति अपने मन के लोभ और कृपणता से सुरक्षित रहा तो ऐसे ही लोग सफल हैं।" (64:16)
ईश्वर ने जो धर्म हमारे लिए उतारा है वह कोई ऐसी दुनिया नहीं जो मात्र विचार और कल्पनाओं से सम्बन्धित हो। धर्म अपने अन्तिम विश्लेषण में सूक्ष्म व्यापार है। लेकिन जिस प्रकार हमारी आत्मा के लिए एक अनुकूल आकार और शरीर प्रदान हुआ है ठीक उसी प्रकार धर्म के लिए भी बाह्य आकार प्रदान किए गए हैं ताकि वास्तविकता मूर्त रूप में निरन्तर हमारे सामने रहे और यह देखने में कोई कठिनाई न हो कि किस व्यक्ति को वास्तव में धर्म मिला है और कौन उससे वंचित है।
धर्म के जिस स्वरूप का उल्लेख यहाँ किया गया है वह वही है जिसे हम नमाज़ और दानशीलता इत्यादि के नाम से याद करते हैं। नमाज़ और दानशीलता दो ऐसे स्पष्ट आकार हैं जिनके द्वारा सत्यधर्म न केवल यह कि सबके लिए बोधगम्य हो जाता है बल्कि उसकी जीती-जागती तस्वीर भी हम देखने लगते हैं। क़ुरआन में है—
“और उन्हें आदेश भी बस यही दिया गया था कि वे अल्लाह की बन्दगी करें, निष्ठा और विनयशीलता को उसके लिए विशिष्ट करके, बिलकुल एकाग्र होकर, और नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें। और यही है सत्यवादी समुदाय का धर्म।” (98:5)
इसमें सन्देह नहीं कि दानशीलता की भावना आदमी को सार्वभौमिकता से जोड़ देती है। इसके द्वारा वह अपने प्रभु से आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। फिर वह इस योग्य हो जाता है कि ईश्वर उसे अपनी समस्त अनुकम्पाओं से अनुगृहीत करे। यह सम्भव नहीं कि बन्दा जीवन के उस मार्ग पर चले जो उसे उच्चतम स्थान तक ले जाता है, फिर भी वह वंचित रहे। इस रूप में तो उसे अनिवार्यतः दोनों लोकों की निधियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन याद रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दौलत चरित्र और व्यक्तित्व की उच्चता ही है। इसके बिना हम किसी महान व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“निश्चय ही सदक़ा ईश्वर के क्रोध को ठंडा करता और बुरी मौत को दूर करता है।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मोमिन उदारता और दानशीलता का स्रोत होता है। यह उसका मौलिक गुण है। यह स्रोत किसी भी परिस्थिति में सूखता नहीं। दानशीलता और सद्क़े से स्वयं दानशील व्यक्ति को भी लाभ पहुँचता है। इससे उसकी आत्मा की शुद्धि होती है और उसका व्यक्तित्व उन्नत होता है। बुरी मौत से ईश्वर उसे सुरक्षित रखता है। बुरी मौत से अभिप्राय ऐसी मौत है कि—
(i) आदमी शान्तिपूर्वक संसार से प्रस्थान न कर सके। मानसिक एकाग्रता उसे प्राप्त न हो।
(ii) तौबा का अवसर न मिले और न अन्तिम समय में कलिमा तय्यिबा मुख से निकाल सके। लौकिक संतापों और लोभ-लिप्साओं से ग्रसित हालत में दुनिया से प्रस्थान करे।
(iii) असत्य के समर्थन में जान दे।
(iv) मौत इस हाल में आए कि वह गुनाह के कामों में व्यस्त हो। दुनिया से ईश्वर का अवज्ञाकारी बन्दा बनकर ईश्वर के सामने जाए।
(v) आत्महत्या कर ले, इत्यादि।
मानव-जीवन में सुन्दर समापन का बड़ा महत्व है। इसलिए कि एतिबार वास्तव में अन्त का ही होता है। यह हदीस बताती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने, उसके क्रोध की आग को बुझाने का सही प्रयास सद्क़ा (दान) है। सद्क़े की बरकत से वह सुन्दर समापन की निधि से भी सम्पन्न हो सकता है।
वास्तव में ईश्वर जिस चीज़ से प्रसन्न होता है वह चरित्र का सौन्दर्य है। इसी का उसके यहाँ महत्व और प्रतिष्ठा है। चरित्र-निर्माण धैर्य और त्याग के बिना सम्भव नहीं है। धैर्य और त्याग के बिना मानव कभी भी अधमता की हालत से नहीं निकल सकता। सद्क़ा चरित्र की महानता का एक स्पष्ट प्रमाण है। सद्क़ा मात्र एक लौकिक कर्म नहीं है, बल्कि वास्तव में यह हृदय की एक अवस्था का नाम है जिसे हम हार्दिक आनन्द या विशाल-हृदयता से अभिव्यंजित कर सकते हैं। यह बड़ी मूल्यवान वस्तु है। यही वास्तविक जीवन है। हमें यह जीवन प्रदान करने के लिए इस्लाम के महान आमन्त्रणदाता हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अन्त तक प्रयासरत रहे।
यह ऐसी पवित्रता है जिसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। इस पवित्रता को धारण करनेवाले व्यक्ति को वह कभी विनष्ट नहीं होने दे सकता। कितनी सही बात कही थी हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने जब उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहले वह्य के अवतरण के अवसर पर परेशान देखा। उन्होंने कहा, “ख़ुदा की क़सम! अल्लाह आप को रुसवा नहीं करेगा। आप तो नाते-रिश्ते का हक़ अदा करते हैं। (कमज़ोरों का) सारा बोझ अपने ऊपर लेते हैं। वंचितों के लिए कमाते हैं। अतिथियों का सत्कार करते हैं। सत्य के लिए मुसीबतें उठाते हैं।”
एक बात यहाँ और समझ लेने की है। वह यह कि केवल भौतिक वस्तुओं के अन्दर ही शक्ति और प्रभाव नहीं पाया जाता (उदाहरणस्वरूप चूने को पानी में डालें तो वह उबलने लगता है, या पानी को आग पर रखिए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है), बल्कि सत्कर्मों और हृदय के विभिन्न भावों में भी शक्ति और प्रभाव पाया जाता है। केवल यही नहीं कि किसी वृक्ष के बीज को मिट्टी में डाल दें तो वह उगता और फिर एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता और फल-फूल लाता है, बल्कि सत्कर्म भी बीज की भाँति होते हैं। ये भी खोकर नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि इस बीज से भी वृक्ष उगते और फल-फूल आते हैं जिनके फलों और छाया से मनुष्य लाभ उठाता है। सत्कर्मों में यह क्षमता होती है कि वे अपना प्रभाव दिखा सकें। अतः ये सत्कर्म अपने प्रभाव से आदमी के मन पर ऐसे चिन्ह छोड़ते हैं और उसके अन्दर ऐसी प्रतिभा का विकास करते हैं कि वह ईमान की सलामती के साथ जीवन के प्रत्येक चरण से गुज़र सके। इसके अतिरिक्त ईश्वर उसके लिए ऐसे साधन उपलब्ध करता है कि वह अन्तिम क्षणों तक सत्यमार्ग पर चलता रहे। कितने ही फ़रिश्ते उसके संगी-साथी और मित्र होते हैं। उनकी संगति से ईमानवालों को बल मिलता है। क़ुरआन में है कि फ़रिश्ते ईमानवालों से कहते हैं—
“हम दुनिया के जीवन में तुम्हारे साथी हैं और आख़िरत में भी।” (41:31)
हम जो कुछ सद्क़ा करते हैं वास्तव में वही हम अपने ऊपर ख़र्च करते हैं। आम दृष्टि में तो आदमी ने जो कुछ अपने खाने-पीने, पहनने इत्यादि में ख़र्च किया वही उसने अपने ऊपर ख़र्च किया। किन्तु वास्तव में आदमी ने जो अच्छे कामों में या दूसरों पर ख़र्च किया वही अपने ऊपर ख़र्च किया। हदीस में आता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब कोई मरता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि उसने आगे क्या भेजा जब कि लोग कहते हैं कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा?" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास आए। उस समय उनके पास खजूर का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा, “ऐ बिलाल! यह क्या है?" उन्होंने कहा कि यह वह चीज़ है जिसे मैंने कल के लिए जमा कर रखा है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या तुम डरते नहीं कि कल क़ियामत के दिन इसके लिए तुम्हें नरकाग्नि के ज्वर का सामना करना पड़े। बिलाल! ख़र्च करो और इसका भय न करो कि अर्शवाले की ओर से तुम्हारे हिस्से में दरिद्रता आ जाए।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
व्याख्या : इस हदीस में इनफ़ाक़ पर बल दिया गया है और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि आदमी का अस्ल भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए। बन्दे का असल भरण-पोषण और उसकी आजीविका का ज़िम्मेदार वही है। ईश्वर महान अर्श का स्वामी है। वह कोई कमज़ोर ईश्वर नहीं है कि बन्दे को आजीविका उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध होगा। अगर आदमी की नीति इससे भिन्न है और वह ईश्वर के बजाए अपने उपाय पर भरोसा करता है और वह अपने कर्म से इसका प्रमाण नहीं देता कि उसका भरोसा ईश्वर पर है तो इसकी आशंका बनी रहती है कि वह आख़िरत में बुरे परिणाम से दोचार हो। बन्दे का भरोसा अपने ईश्वर पर है। जीवन में इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह सद्क़ा है जो वह ईश्वरीय मार्ग में देता है। सद्क़ा और दानशीलता से बचना मोमिन की नीति कदापि नहीं हो सकती।
आदमी भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कुछ जमा करता है तो इसमें धार्मिक दृष्टि से कोई बुराई नहीं है। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) वास्तव में अपने सहाबियों को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके जीवन में किसी दुर्बलता के प्रवेश करने की सम्भावना शेष न रहे।
दृष्टिकोण
(1) हज़रत अबू-मूसा अश-अरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"हृदय की उपमा एक पंख की-सी है जो किसी खुले मैदान में पड़ा हुआ हो। हवाएँ उसे उलट-पलट रही हों।" (हदीस : इब्ने-माजा)
इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मानव-हृदय की एक अनोखी उपमा दी है। इससे जीवन के बहुत-से तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। इस मिसाल के कई अंश हैं—
(i) खुला हुआ मैदान जहाँ बेरोक-टोक हवाओं का गुज़र होता है। फिर ऐसे मैदान में छोटी चीज़ भी पड़ी हो तो वह अपनी ओर हमारी दृष्टि को आकर्षित कर लेती है।
(ii) उस खुले मैदान में एक पंख पड़ा हुआ है। उसे उठानेवाला कोई नहीं। कोई नहीं जो उसे उठाकर किसी सुरक्षित ताक़ में रख दे या अपने इस्तेमाल में ले आए।
(iii) उस पंख को छेड़नेवाली और उस तक पहुँचनेवाली कोई चीज़ अगर है तो वे हवाएँ हैं। कभी धीमी हवा उस तक आती है तो कभी तेज़ हवा उसपर से गुज़रती है। कभी पिछले पहर की मन्द वायु धीमी गति से उसके पास आती है तो कभी तूफ़ानी हवाएँ उस तक पहुँचती हैं। तात्पर्य यह कि विभिन्न प्रकार की हवाओं से उसका सामना होता रहता है।
(iv) हवाएँ आकर उसे उलटती-पलटती रहती हैं।
इस मिसाल के द्वारा निस्सहायता और निस्पृहता का अत्यन्त प्रभावकारी चित्रण किया गया है। हवाएँ आती हैं और उसे उलट-पलट करती हैं। मानव का हृदय भी एक ऐसे ही पंख के समान है। दुनिया के इस मैदान में मानव-हृदय एक गिरे हुए पंख की भाँति है जिसे चलनेवाली हवाएँ प्रभावित करती हैं। उसे एक अवस्था में पड़ा नहीं रहने देतीं। दिल के इस उलट-फेर की अभिव्यक्ति मानव-जीवन में विभिन्न रूपों में होती है। हदीस के टीकाकारों ने इस उपमा से यह अर्थ निर्गत किया है कि इसमें इस वास्तविकता को प्रकट किया गया है कि दुनिया में मानव से जो भी कार्य होता है वह नियति के अनुसार होता है। हृदय तो किसी खुले मैदान में पड़े हुए पंख की भाँति है, उसमें जो कुछ भी गति होती है वह वास्तव में नियति का कार्यान्वयन एवं प्रदर्शन मात्र है। एक दूसरी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लोगों के हृदय दयावान ईश्वर की अंगुलियों में से दो अंगुलियों के मध्य मात्र एक हृदय की भाँति हैं, वह जिस प्रकार चाहता है उसे उलटता-पलटता रहता है।” फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “ऐ अल्लाह, दिलों के फेरनेवाले, हमारे दिलों को अपनी आज्ञाकारिता की ओर फेर दे।”
इन हदीसों में मानव की बेचारगी और बेबसी और ईश्वर की जिस बड़ी क़ुदरत का उल्लेख किया गया है उससे यह नतीजा निकालना कदापि सही नहीं होगा कि मानव बिल्कुल ही मजबूर और विवश है। अपने कर्म और व्यक्तित्व और विचारों में उसका अपना कोई नहीं है। क्योंकि इस सूरत में न तो बहुदेववादी और अवज्ञाकारी लोग निन्दित ठहरेंगे और न नेक काम करनेवाले आज्ञाकारी बन्दे किसी प्रशंसा के योग्य समझे जा सकते हैं। क़ुरआन की ये आयतें भी निरर्थक सिद्ध होंगी—
“प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई के साथ बंधा हुआ है।" (76: 38)
“हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले में बन्धक है।" (52:21)
इससे ज्ञात हुआ कि नियति से आदमी के संकल्प और कर्म की स्वतन्त्रता समाप्त नहीं हो जाती। बल्कि भाग्य की अवधारणा से आदमी के संकल्प और चुनाव की स्वतन्त्रता ही की पुष्टि होती है। अतः अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से जब पूछा गया कि जो झाड़-फूँक और दवा-इलाज हम करते हैं और बचाव और सुरक्षा की जो युक्तियाँ हम अपनाते हैं, क्या ये चीज़ें ईश्वर द्वारा निर्धारित भाग्य को बदल देती हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ये चीज़ें भी ईश्वर द्वारा नियत भाग्य ही में सम्मिलित हैं।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
मतलब यह कि ईश्वरीय नियति से दवा-इलाज का निषेध नहीं होता। ईश्वरीय नियति में ये चीज़ें भी सम्मिलित हैं। ईश्वरीय नियति में इन चीज़ों का लिहाज़ रखा गया है।
हृदय के पंख को बाह्य हवाएँ अगर उलटती-पलटती हैं तो उनकी यह क्रिया किसी महत्वपूर्ण क़ानून के तहत ही होती है। दयावान ईश्वर अगर अपनी अंगुलियों से हृदयों को फेरता है तो उसका यह कार्य यूँ ही अन्धाधुन्ध नहीं होता। वह ऐसे हृदयों को कुफ़्र और अवज्ञाकारिता की ओर नहीं फेरता जिनमें आज्ञाकारिता और ईश्वरीय प्रसन्नता की चाह होती है बल्कि ऐसे हृदयों को तो वह अपनी आज्ञाकारिता की ओर ही फेरेगा। अलबत्ता जिन दिलों में कुफ़्र और अवज्ञाकारिता के रुझान पाए जाते हैं उनको वह कुफ़्र और अवज्ञाकारिता की तरफ़ फेरेगा। वह ज़ोर-ज़बरदस्ती से न तो किसी को आज्ञाकारिता और वफ़ादारी की ओर खींचता है और न ही कुफ़्र और गुनाह की ओर फेरता है।
मानव का हृदय एक अत्यन्त संवेदनशील यन्त्र के सदृश है जिसके अन्दर यह सामर्थ्य पाई जाती है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को महसूस कर सके। दुनिया में जो घटनाएँ घटती हैं उनका प्रभाव अनिवार्यतः हमारे हृदय पर पड़ता है। लेकिन विभिन्न हृदयों पर उनके प्रभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक घटना से ईमानवाले के ईमान में वृद्धि होती है लेकिन उसी घटना से कपटाचारियों के हृदय आतंकित और भयभीत हो जाते हैं और उनकी शान्ति भंग होकर रह जाती है।
बहुत-सी घटनाओं की सूचना हमें रेडियो और समाचारपत्रों के द्वारा मिलती है। हमारे हृदयों पर उनका अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के वातावरण में बेहद चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। आज के वातावरण में कितनी ही उपद्रवकारी वस्तुएँ मौजूद हैं जिनसे सभी परिचित हैं। काम भावनाओं को भड़कानेवाले फ़िल्मी गीत, टेलीवीज़न के परदे पर प्रस्तुत किए जानेवाले लज्जास्पद और अश्लील दृश्य, ये और इस प्रकार की दूसरी चीज़ें और पथभ्रष्ट नेताओं के कपटपूर्ण भाषण— इन सबकी ओर से सावधान रहना आवश्यक है कि कहीं ये चीज़ें हमारे दिलों को ग़लत दिशा में न फेर दें और हमारी धार्मिक अभिरुचि को बिगाड़कर न रख दें।
इनसानों में पाए जानेवाले शैतानों के अतिरिक्त जिन्नों में पाए जानेवाले शैतानों के प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शैतान दिलों में विभिन्न प्रकार की शंकाएँ डालने का प्रयास करता है लेकिन ईश्वर के निष्ठावान बन्दों पर उसका जादू नहीं चल सकता। और अगर कभी वह किसी हद तक उन्हें प्रभावित करता भी है तो वे शीघ्र ही सतर्क हो जाते हैं और ईश्वर की ओर पलटते और उसकी शरण में आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होता है वे बहुत जल्द शैतान के बहकावे में आ जाते हैं।
ईश्वर के फ़रिश्ते भी अपना प्रभाव हृदयों पर डालते हैं। हृदयों में कभी अच्छे विचार और भाव भी वे डालते हैं। ईश्वर के नेक बन्दों को इससे बड़ा बल मिलता है।
फिर जिस प्रकार वर्तमान संसार के प्रभाव दिलों पर हैं उसी प्रकार दिव्यलोक के प्रभाव भी मानव हृदय पर पड़ते हैं। ईश्वर जिस किसी से प्रेम करता है वह उच्चलोक के फ़रिश्तों में प्रिय बन जाता है और फिर वहाँ से धरती पर उसकी लोकप्रियता उतरती है और लोगों की दृष्टि में उसका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रिय हो जाता है जैसा कि एक हदीस में इसे स्पष्ट किया गया है।
इस सम्बन्ध में इस तथ्य को भी दृष्टि में रखना होगा कि ईश्वर स्वयं मूल्यवान हृदयों को प्रशिक्षित करता है। उसपर पारलौकिक शान्ति और दयालुता की वर्षा होती है। पारलौकिक कृपादानों के द्वारा ईश्वर अपने निष्ठावान और वफ़ादार बन्दों की मदद करता है। क़ुरआन में कहा गया है—
"वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को अंकित कर दिया है और अपनी ओर से एक आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दी है।" (58:22)
ईश्वर उनके हृदयों में अडिगता और दृढ़ता की शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो ईमान लाने से मुख फेरता और ईश्वरीय मार्गदर्शन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति को भटकने के लिए छोड़ देता है। उसके लिए वही मार्ग सरल कर देता है जिसपर वह चलना चाहता है। (92 : 8-10)
ईमानवालों के हृदयों को वह गुमराही और अन्धकार से बचाता और उनको सत्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है—
“और जो कोई ईश्वर पर ईमान रखता है तो वह उसके दिल को मार्ग दिखा देता है (भटकने के लिए नहीं छोड़ता)।” (64 :11)
यूँ तो ईश्वर की ओर से कृपादानों और अनुकम्पाओं की वर्षा होती ही रहती है लेकिन इसकी कुछ विशेष घड़ियाँ भी हैं जिनमें विशेष रूप से इबादत और प्रार्थना की शिक्षा दी गई है। धन्य हैं वे लोग जिनके हृदय ईश्वरीय अनुकम्पाओं और अनुग्रहों की वर्षा से लाभान्वित होते रहते हैं और हानिकारक हवाओं के कुप्रभावों का मुक़ाबला करने की उनके अन्दर शक्ति होती है जिसके कारण हर प्रकार के बुरे प्रभावों से उनके हृदय सुरक्षित रहते हैं और अगर उनके हृदयों पर कोई ग़लत प्रभाव पड़ भी जाता है तो शीघ्र ही उनका हृदय उन प्रभावों को दूर कर देता है, उनको अपने अन्दर किसी भी क़ीमत पर शेष नहीं रहने देता।
यह एक तथ्य है कि मानव अपने हृदय की प्रवृत्तियों के अधीन होता है। हृदय के ठीक होने पर ही जीवन का कल्याण निर्भर करता है। आख़िरत की सफलता भी वास्तव में हृदय के स्वस्थ होने पर ही निर्भर है। अतएवः क़ुरआन में कहा गया है—
"जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद सिवाय इसके कि कोई भला-चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के पास आया हो।” (26: 88-89)
एक दूसरी जगह कहा गया है—
“यह है वह चीज़ (अर्थात स्वर्ग) जिसका तुमसे वादा किया जाता था प्रत्येक रुजूअ करनेवाले, बड़ी निगरानी रखनेवाले के लिए; जो रहमान से डरा परोक्ष में और आया रुजूअ रहनेवाला हृदय ले कर।" (50 : 32-33)
इस अवसर पर इतिहास की उस महान घटना पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए जब दुनिया में अधर्म और अन्धकार व्याप्त था। मानव-हृदयों पर अधर्म का घोर आक्रमण हो रहा था, ईश्वर को मानव हृदयों की इस क्षत-विक्षत अवस्था पर दया आई और उसने वह्य (प्रकाशना) के रूप में रहमत की हवा भेजी। इस सिलसिले में परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों साधनों का उपयोग किया गया। हज़रत जिबरील (अलैहिस्सलाम) जैसे ईश्वर के सतत सानिध्य में रहनेवाले फ़रिश्ते को इस कार्य पर नियुक्त किया गया जो एक प्रत्यक्ष प्राणी न थे। और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जैसे सज्जन हृदय व्यक्ति को रिसालत के लिए चुना गया जो इन्सानी दुनिया से सम्बन्ध रखनेवाले एक व्यक्ति थे। अधर्म और अन्धकार के मुक़ाबले में रहमत की हवाएँ भी स्पष्ट रूप से चलीं और पूरे तेईस वर्षों तक चलती रहीं। इतिहास ने देखा कि इस मंगलकारी हवा ने कितने ही हृदयों को परिवर्तित कर दिया। कितने ही हृदय हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो गए। रहमत की इस हवा से उन्हीं लोगों के हृदय वंचित रहे जिनमें गम्भीर क़िस्म का रोग था और वे इस रोग को पाले ही रखना चाहते थे। ईश्वर की यह रहमत क़ुरआन के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। क़ुरआन का प्रभाव ग्रहण करने के बाद हृदयों में जो भाव उत्पन्न होता है और उनकी जो दशा होती है वही उनके स्वस्थ होने का लक्षण है। इसके विपरीत हृदयों की अन्य दशाओं और भावों को कदापि प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।
क्षमा
(1) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते सुना—
"जिस व्यक्ति के शरीर को ज़ख़्मी किया गया हो और वह उसको क्षमा कर दे जिसने उसे ज़ख़्मी किया हो तो अल्लाह अनिवार्यतः उसका दर्जा उँचा कर देता और उसके गुनाह क्षमा कर देता है।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिसे ज़ख़्म पहुँचाया गया हो, उस आदमी को जिसने उसे ज़ख़्मी किया, क्षमा कर दे और कोई बदला न ले हालाँकि बदला लेने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है तो उसका यह व्यवहार अत्यन्त पसन्दीदा है। आघात पहुँचानेवाले को क्षमा करके वास्तव में वह इस बात का परिचय देता है कि वह लोगों के सामान्य नैतिक स्तर से उच्च है। उसके अन्दर धैर्य और सहनशीलता की असाधारण शक्ति पाई जाती है। बदला और प्रतिशोध से अधिक प्रिय उसे अपनी सुरुचि और नैतिक उदारता है। अल्लाह को यह चीज़ इतनी प्रिय है कि वह न केवल यह कि उसकी इस उच्चता और महानता की रक्षा करता और उसे इस स्थान से गिरने से बचाता है बल्कि जीवन में स्वयं उस व्यक्ति से जो भूल-चूक और ग़लती हुई होती है उसे भी क्षमा कर देता है। यह एक तथ्य है कि आदमी अगर ईश्वर के किसी बन्दे के साथ उदारता से काम लेता है तो अनिवार्यतः ईश्वर भी उसके साथ उदारता से ही पेश आएगा।
करुणा
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी पत्नियों और उम्मे-सुलैम के सिवा किसी महिला के पास नहीं जाते थे। आप उम्मे-सुलैम के यहाँ जाया करते थे। लोगों ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इसका कारण पूछा तो कहा, "मुझे उसपर अत्यन्त दया आती है, उसका भाई मारा गया जबकि वह मेरे साथ था।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत उम्मे-सुलैम (रज़ियल्लाहु अन्हा) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) की माँ और हज़रत अबू-तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की पत्नी थीं। वे वास्तव में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दूध या वंश सम्बन्धी मौसी होती थीं जैसा कि इमाम नववी (रहमतुल्लाह अलैह) ने इसे स्पष्ट किया है, और महरम होने के कारण आपके लिए उनके यहाँ जाने में कोई हर्ज न था। (महरम वह है जिससे पर्दा करने की आवश्यकता नहीं होती।)
इस हदीस से सिद्ध होता है कि मानवीय आचरण में दया और करुणा का बड़ा महत्व है और यह वास्तव में पैग़म्बरों का आचरण है।
जो हृदय करुणा से वंचित हो वह अत्यन्त संवेदनहीन और निष्प्राण होगा। हृदय तो करुणा और दयाभाव ही का नाम है। यह चीज़ अगर हृदय में न हो तो हृदय का होना न होना बराबर है। दया, करुणा और सहानुभूति की भावना अगर हृदय में मौजूद है तो समझिए कि हृदय जीवित है, अन्यथा वह मृत है। उससे किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती।
नर्म स्वभाव
(1) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पत्नी हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ आइशा! अल्लाह नर्म स्वभाव का है, नर्म स्वभाव को पसन्द करता है और नर्मी पर वह कुछ प्रदान करता है जो कठोरता पर प्रदान नहीं करता, और न नर्म स्वभाव के सिवा किसी दूसरे गुण पर प्रदान करता है।” (मुस्लिम)
व्याख्या : सहीह बुख़ारी की एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह नर्म स्वभाव का है और हर मामले में नर्मी को पसन्द करता है।”
इस हदीस से नर्म स्वभाव और नर्म नीति अपनाने की महत्ता और श्रेष्ठता का पता चलता है। जब नर्मी स्वयं ईश्वर का गुण है तो उसके महत्व से किसे इन्कार हो सकता है। नर्मी के अन्दर ईश्वर ने बड़ी समाई और बरकत रखी है। नर्मी के द्वारा इन्सान वे लाभ प्राप्त कर सकता है जो सख़्ती के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए स्वयं इन्सान के अपने हितों के लिए भी अपेक्षित है कि वह आपस के मामलों में नर्मी और मेहरबानी का रवैया अपनाए। अल्लाह को जो बात प्रिय हो सकती है वह यही है कि उसके बन्दे परस्पर एक-दूसरे पर मेहरबान हों। वे एक-दूसरे के लिए कदापि कठोर न हों। वे अपने बरताव और व्यवहार में नर्मी के पहलू को हमेशा दृष्टि में रखें। इससे जो सांसारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं वे तो प्राप्त होंगे ही, इससे स्वयं अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को भी लाभ पहुँचेगा। इसकी ओर साधारणतः लोगों की दृष्टि नहीं जाती कि नर्मी वास्तव में चरित्र और व्यक्तित्व का सौन्दर्य है। और फिर इससे इन्सान को हार्दिक सुख-शान्ति की जो अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा सम्भव नहीं। नर्मी का आकर्षण और उसकी मोहकता अत्यन्त भरोसेमन्द, विश्वसनीय और प्रभावोत्पादक होती है। इसके जो प्रभाव दूसरों के दिलों पर अंकित होते हैं वे मिटाए नहीं मिटते।
Soft is the music that would charm forever.
(2) हज़रत जरीर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति नर्म स्वभाव से वंचित है वह समस्त भलाइयों से वंचित है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में नर्मी को बुनियादी महत्व प्राप्त है। इनसान की अधिकांश भलाइयों और गुणों का स्रोत उसके स्वभाव की मृदुलता है। इसलिए नर्मी का अभाव हर प्रकार की भलाई से वंचित होना है।
आप सामाजिक पहलू से विचार करें। अगर आदमी में नर्मी का तत्व नहीं है तो वह कमज़ोरों, वृद्धजनों और अपने मातहतों के साथ बरताव करने में असफल सिद्ध होगा जिसके वे अधिकारी होते हैं। मजबूरों और बेकसों की आशाएँ वही व्यक्ति पूरी कर सकता है जिसके हृदय में करुणा हो, जिसे दूसरों के कष्टों और उनकी आवश्यकताओं का एहसास हो। और यह एहसास ऐसा हो कि उसे बेचैन कर सके। संवेदनशील हृदय रखनेवालों के कान भी अत्यन्त संवेदनशील होते हैं, वे उन आवाज़ों को भी सुन लेते हैं जो मजबूरों के दिलों में दबी होती हैं और उनके मुख तक नहीं आतीं। वे उस बेकसी और निस्सहायता की अवस्था का भी अनुभव कर लेते हैं जिसमें कोई निर्धन और दीन-हीन व्यक्ति पड़ा होता है। कमज़ोरों और वृद्धजनों के साथ नर्म बरताव और उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसी प्रकार जो लोग अपने अधीन हों उनके साथ उपकार की नीति अपनानी चाहिए। उनसे उनकी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक काम न लिया जाए और प्रयास इस बात का हो कि हम उन्हें उनकी निर्धारित मज़दूरी से ज़्यादा दे सकें। उनके साथ इनसानियत का सुलूक करें। उनके आत्मसम्मान और मर्यादा को ठेस न पहुँचाएँ। उनका साहस बढ़ाएँ। अगर उनके अन्दर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो युक्तिपूर्ण ढंग से उनके सुधार की भी कोशिश करें। सज्जनता नर्मी और करुणा में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि उसके द्वारा पाषाण-हृदयों को भी मोम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उदारता आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस रहस्य से अवगत हों कि आदमी के लिए प्रतिष्ठा की बात वास्तव में यह है कि उसके अन्दर धैर्य और सहनशीलता और नर्मी के तत्व पाए जाते हों। दिलों को आराम पहुँचाने में उसे आराम मिलता हो। यही चीज़ आदमी को ईश्वर की दृष्टि में ऊँचा बनाती है। मनुष्य का सम्पूर्ण अहंकार और दंभ समाप्त होकर रहता है लेकिन अच्छे चरित्र के चिन्ह ऐसे होते हैं कि जो मिटाए नहीं मिटते। लोग केवल मदिरा के स्वाद और उसकी मस्ती को जानते हैं या फिर खाने-पीने के स्वाद से परिचित होते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो आनन्द सत्कर्म और नैतिक सौन्दर्य में रखा है वह आनन्द कहीं और नहीं पाया जाता।
एक बुनियादी चीज़ हमेशा हमारी दृष्टि में रहनी चाहिए। इससे धर्म को समझने में आसानी होगी। प्रत्येक चीज़ का एक उद्गम और स्रोत होता है। उदाहरणस्वरूप हवा हमारी आवश्यकता है। हम हवा में साँस लेते हैं। हवा का एक विपुल भण्डार है जो हमसे कुछ भी दूर नहीं। हम उस भण्डार से हवा प्राप्त करते रहते हैं। इसी प्रकार शारीरिक तत्वों का स्रोत यह धरती है जिससे हमें ये तत्व प्राप्त होते हैं। जब हम साँस लेते हैं तो एक व्यापक वायुमंडल से हमारा सम्पर्क हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे अन्दर प्रेम, दया और करुणा की भावनाएँ उभरती हैं और हम उन भावनाओं के महत्व और मूल्य को समझते हैं और उन्हें दबाते नहीं बल्कि कमज़ोरों, मजबूरों और ज़रूरतमन्दों के काम आते हैं तो वास्तव में उस समय प्रतापवान और महान ईश्वर के प्रकाश से हम रश्मित हो रहे होते हैं जो दया और कृपा का मूल उद्गम और स्रोत है। जहाँ कहीं जिस रूप में भी दयालुता के चिन्ह पाए जाते हैं वे उसी की दयालुता के अंश होते हैं। जिस किसी का सम्बन्ध ईश्वर से स्थापित हो जाता है तो ईश्वर उसपर अपनी अनुकम्पा और दया दर्शाता है। उसकी ओर पूर्णतः उन्मुख होता है और उसे अनुग्रहीत करता है यहाँ तक कि उसे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाता है, वह स्वर्ग जो ईश्वरीय अनुकम्पा की पूर्ण अभिव्यक्ति है।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा—
“नर्मी को अपने ऊपर अनिवार्य जानो और कठोरता और अश्लीलता से बचती रहो। इसलिए कि नर्मी जिस चीज़ में होती है वह उसे सुन्दर बना देती है और जिस चीज़ से नर्मी अलग कर ली जाती है वह ऐबदार हो जाती है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अबू दाऊद की एक हदीस में ये शब्द आए हैं—
“ऐ आइशा! नर्मी अपनाओ।”
किसी वस्तु में सुन्दरता का पाया जाना उसके ठीक और प्रिय होने का एक स्पष्ट प्रमाण है। इससे यह भी ज्ञात हुआ कि नर्मी और कोमलता केवल फूलों की शोभा नहीं है बल्कि मानवीय नैतिकता और कार्य-व्यापार में भी इससे आकर्षण और सौन्दर्य उत्पन्न होता है। जिस गुण के न होने के कारण कोई चीज़ बिगड़ जाती और दोषपूर्ण हो जाती हो उसकी आवश्यकता और महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐबदार वस्तु से हम भलाई की आशा नहीं कर सकते। भलाई के लिए आवश्यक है कि हम जीवन में मृदुलता और नर्म व्यवहार की कभी उपेक्षा न करें।
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
“अल्लाह किसी घर के लोगों के लिए नर्मी प्रदान करने का इरादा करता है तो अनिवार्यतः इसके द्वारा उन्हें लाभ पहुँचाता है और इसके विपरीत जिस किसी घर के लोगों को नर्मी से वंचित रखता है तो अनिवार्यतः उनको हानि पहुँचाता है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : किसी घर के व्यक्तियों में अगर नर्मी का गुण पाया जाता है तो यह अत्यन्त शुभ है। इसके कारण घर स्वर्ग-समान हो जाता है। घर में एक आकर्षक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। शील-स्वभाव और व्यवहार की विनम्रता से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए सुख-चैन का कारण होगा। उनमें परस्पर प्रेम की भावना कार्यरत होगी। घर का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का शुभचिन्तक होगा। इसके विपरीत अगर घर के लोगों में नर्मी की जगह कठोरता और तीक्ष्ण स्वभाव पाया जाता है तो इससे अनिवार्यतः यह होगा कि घर के लोग हमेशा एक प्रकार की यातना में ग्रस्त होंगे। घर का वातावरण प्रदूषित होकर रहेगा। लोग मानसिक तनाव में जी रहे होंगे। घर के लोगों में एक-दूसरे के लिए प्रेम और सौहार्द की जगह ईर्ष्या और द्वेष की भावना पलेगी। घर का सुख-चैन जाता रहेगा। पारलौकिक जीवन में इसके कारण जो हानियाँ होंगी वे तो होंगी ही।
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति को नर्मी का कोई अंश मिला उसे दुनिया और आख़िरत की भलाई नसीब हुई और जिस व्यक्ति को नर्मी नसीब न हुई वह दुनिया और आख़िरत की भलाई से वंचित रहा।" (हदीस : अल-बग़वी फ़ी शरहिस्सुन्नह)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि जीवन चाहे दुनिया का हो या आख़िरत का, उसका स्वभाव और प्रवृत्ति एक है। जो चीज़ दुनिया के जीवन पर प्रभाव डालती है आख़िरत के जीवन पर भी वह उसी अन्दाज़ से अपना प्रभाव डालती है। दुनिया और आख़िरत में जो ख़ैर और भलाई है उसकी प्राप्ति का साधन एक विशेष नैतिक व्यवहार है। जीवन में इस नैतिक व्यवहार को कृत्रिम रूप में नहीं अपनाया जा सकता। उसके लिए आवश्यक है कि आदमी के स्वभाव में नर्मी हो, कठोरता न हो। स्वभाव की यही मृदुलता और नर्मी आदमी के काम को आसान कर देती है और वह स्वभावतः उस आचरण और व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है जिसके कारण दुनिया और आख़िरत की भलाइयाँ उसके हिस्से में आती हैं। ऐसा व्यक्ति न दुनिया में भलाई से वंचित रहता है और न आख़िरत में उसे असफलता और निराशा का मुँह देखना पड़ सकता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति स्वभाव का कठोर और सख़्त और तीखे मिज़ाजवाला है तो यह चीज़ उसे दुनिया में भी वास्तविक सुख-चैन, शान्ति और भलाई से वंचित रखेगी और आख़िरत में भी असफलता और निराशा की मंज़िल तक पहुँचाकर रहेगी।
विनम्रता और करुणा एक बुनियादी गुण और भलाइयों का स्रोत है। इसका प्रमाण इस हदीस से भी मिलता है जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यमनवालों के बारे में कहा—
“वे लोग हृदय के अत्यन्त नर्म होते हैं। ईमान, दीन की समझ और हिक्मत तो यमन ही का हिस्सा है।" (हदीस : मुस्लिम)
अर्थात कठोर हृदयता से वे मुक्त हैं। वे अपनी नर्मी के गुण के कारण ईमान, दीनी समझ और तत्वदर्शिता से सम्पन्न हुए हैं।
(6) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या मैं तुम्हें उस व्यक्ति की सूचना न दूँ जो नरकाग्नि के लिए हराम है और जिसपर नरकाग्नि हराम है। (नरक हराम है) प्रत्येक उस व्यक्ति पर जो विनम्र प्रवृत्ति, नर्म स्वभाव, क़रीब होनेवाला, आसानी से पेश आनेवाला है।" (हदीस : अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में जिन चार गुणों का उल्लेख किया गया है वे अर्थ में एक-दूसरे से निकट हैं और नर्मी के विभिन्न पक्षों को सामने लाते हैं। हदीस का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वभाव का नर्म और मुरव्वत रखनेवाला हो और हर प्रकार की कृत्रिमता से मुक्त होकर लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आता हो, न तो वह लोगों से दूर रहता हो और न लोगों ही को उससे निकट होने में कोई संकोच और झिझक होती हो तो यह इस बात का सूचक है कि उस व्यक्ति पर नरक की आग हराम है। क्योंकि ये गुण जिनसे वह सुसज्जित है स्वर्गवालों के गुण हैं। अलबत्ता इस प्रकार की शुभ-सूचनाओं के सिलसिले में यह बात दृष्टि में रहनी चाहिए कि इनका सम्बन्ध हमेशा उन लोगों से होता है जो मोमिन हों, इनकारी न हों और धर्म की अनिवार्यताओं की ओर से बेपरवाह न हों। इस प्रकार के शुभ समाचारों के साथ कुछ शर्तें निहित हुआ करती हैं।
सुसमाचार अधर्मियों के लिए नहीं हुआ करते और न उन लोगों के लिए होते हैं जो धर्म की अपेक्षाओं से सर्वथा विमुख होकर जीवनयापन करते हों, और ईमान के बिना तो ईश्वर के यहाँ किसी भी कर्म और आचरण का कोई मूल्य नहीं हो सकता।
करुणा एवं दयालुता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब ईश्वर ने सृष्टिजन को पैदा किया तो अपनी किताब में लिखा। वह अपने विषय में लिखता है— और वह लेख उसके पास अर्श पर रखा हुआ है— मेरी रहमत मेरे प्रकोप पर प्रभावी है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मुस्लिम की एक हदीस में ईश्वर का यह कथन उद्धृत हुआ है—
“मेरी दयालुता को मेरे क्रोध पर अग्रसरता प्राप्त है।"
रहमत ईश्वर का विशेष गुण है। इसलिए बन्दों का भी कर्तव्य है कि वे अपने जीवन के मामलों में हमेशा करुणा और रहमदिली का रवैया अपनाएँ। किसी मामले में सख़्ती केवल उसी समय करनी चाहिए जब उसके सिवा कोई उपाय शेष न रहे, अन्यथा जीवन के आम मामलों में नर्मी और दयालुता से ही काम लेना वास्तविक पौरुष है। आदमी का व्यक्तित्व भी आकर्षक और मनमोहक तभी हो सकता है जबकि नर्मी और दयालुता के गुण उसमें स्पष्टतया उभरे हुए हों।
(2) हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर उस व्यक्ति पर दया नहीं करता जो लोगों पर दया नहीं करता।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस अर्थ की कई हदीसें उल्लिखित हैं, उदाहरण स्वरूप नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो दया नहीं करेगा तो ईश्वर भी उसपर दया नहीं करेगा" (हदीस : मुस्लिम)
“जो लोगों पर दया नहीं करेगा तो ईश्वर भी उस पर दया नहीं करेगा।” (हदीस : मुस्लिम)
एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति हमारे छोटों पर दया न करे और कृपादृष्टि न रखे और हमारे बड़ों के अधिकार न पहचाने वह हममें से नहीं है। (हदीस : अबू-दाऊद, हाकिम)
अहमद और तिर्मिज़ी में उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति हममें से नहीं है (अर्थात वह हमारे तरीक़े पर नहीं है) जिसने बड़े का आदर न किया और न छोटे पर दया की और न भलाई का आदेश दिया और न बुराई से रोकने का दायित्व निभाया।"
एक और हदीस है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"रहम करनेवालों पर रहमान रहम करेगा, तुम ज़मीनवालों पर रहम करो, तुमपर वह रहम करेगा जो आसमान में है।"
एक हदीस में ‘अहलल-अर्ज़’ (अर्थात ज़मीनवालों) के बजाए ‘मन फ़िल-अर्ज़’ (अर्थात ज़मीन में रहनेवाले लोग) आया है। मगर अर्थ दोनों का एक ही है।
इन हदीसों से यह भली-भाँति सिद्ध होता है कि ईश्वरीय अनुकम्पा और उसकी दयादृष्टि का पात्र बनने के लिए आवश्यक है कि हम उसके बन्दों के लिए दयावान बनें। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर की रहमत हमारे हिस्से में आएगी और अगर कहीं हमारा रवैया इससे भिन्न हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि हम स्वयं ईश्वर के अनुग्रहों और उसकी दया से अपने आप को वंचित रखना चाहते हैं।
हदीस में अन्नास शब्द आया है जिसमें मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम सब सम्मिलित हैं। हमारी दया और कृपा के पात्र सभी हैं, बल्कि ग़ैर-मुस्लिम और ईश्वर के अवज्ञाकारियों के लिए तो हमारे अन्दर और भी ज़्यादा बेचैनी और चिन्ता होनी चाहिए कि वे किसी प्रकार कुफ़्र से बाज़ आ जाएँ और ईश्वर की यातना से बच सकें।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। वे वर्णन करती हैं कि एक देहाती नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ और (सहाबा को बच्चों को प्यार करते और उनका चुंबन लेते देखकर) कहा कि क्या आप लोग बच्चों का चुंबन लेते हैं। हम लोग तो उनका चुंबन नहीं लेते। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “फिर तुझ पर मेरा क्या वश हो सकता है जबकि अल्लाह ने तेरे हृदय से रहमत निकाल ली है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मैं ऐसी हालत में क्या कर सकता हूँ जबकि ईश्वर ने तेरे दिल से रहमत छीन ली है। मुझे यह अधिकार तो प्राप्त नहीं कि जिस चीज़ को ईश्वर तेरे दिल से निकाल ले मैं उसे तेरे दिल में रख दूँ या सिरे से तेरे दिल से रहमत को निकलने ही न दूँ।
इस हदीस में वास्तव में यह एहसास कराया गया है कि बच्चों से प्यार और मुहब्बत से पेश आना और उनका चुंबन लेना आदमी की अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कदापि नहीं है, बल्कि यह तो वह रहमत है जिसे लोगों के दिलों में ईश्वर ने रख दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी नादानी और नासमझी के कारण इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझने लग जाए तो इस स्थिति में ईश्वर को इसकी परवाह नहीं होती। उसका दिल कठोर और दया और करुणा की भावना से सर्वथा रिक्त हो जाता है। इसमें दोष उसका अपना होता है। इसके लिए वह किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता। अतएव एक हदीस में आता है, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“रहमत बस अभागे से ही छीनी जाती है।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी, अहमद)
अभागा है वह व्यक्ति जिसका दिल रहमत जैसे तत्व से वंचित है।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“अल्लाह ने रहमत के सौ भाग किए, फिर निन्यानवे भाग अपने पास रखे और एक भाग धरती में उतारा। प्राणी जो एक-दूसरे पर रहम करते हैं वे इसी एक भाग के कारण करते हैं। यहाँ तक कि घोड़ा भी अपने बच्चे पर से इस डर से पैर उठा लेता है कि उसे कष्ट न हो।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : उपमा के रूप में कहा गया है कि ईश्वर ने अपनी रहमत का सौवां भाग (1/100) ही धरती में उतारा है। रहमत का शेष भाग उसके अपने पास मौजूद है ताकि लोग एक ओर उसकी रहमत की क्रियाशीलता और उसके प्रभावों का अवलोकन कर सकें और दूसरी ओर वे ईश्वर की उस रहमत के उम्मीदवार बनें जो उसने अपने पास रोक रखी है। ईश्वर के पास जो रहमत है, जिसकी अभिव्यक्ति आख़िरत की दुनिया में होगी वह दुनिया में प्रकट होनेवाली रहमत का केवल सौ गुना हो ऐसा नहीं है और न हदीस का अभिप्राय ही यह है। ईश्वर के पास जो रहमत है वह असीमित है। असीमित की सीमित से क्या तुलना की जा सकती है। यह उपमा केवल यह बोध कराने के लिए प्रस्तुत की गई है कि ईश्वर की जो रहमत दुनिया में अवतरित हुई है वह उस रहमत की तुलना में अत्यन्त ही अल्पमात्रा में है जो उसके अपने पास मौजूद है। इस थोड़ी-सी रहमत का प्रभाव यह है कि ईश्वर द्वारा सृष्ट प्राणियों में रहमत और तरस की भावना पाई जाती है। इनसान तो इनसान, जानवरों तक में रहमत के लक्षण स्पष्ट हैं। किसी जानवर का, उदाहरणार्थ घोड़े का पैर असावधानीवश अगर उसके अपने बच्चे पर पड़ जाता है तो वह फ़ौरन ही अपना पैर बच्चे पर से उठा लेता है कि बच्चे को कष्ट न हो।
सोचने की बात यह है कि ईश्वर अपनी रहमत को पूर्णतया प्रकट करेगा तो फिर उसके प्रभाव क्या और किस रूप में प्रकट होंगे, इसकी तो आज हमारे लिए सही तौर पर कल्पना करना भी सम्भव नहीं है।
जानवरों पर दया
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“एक व्यक्ति रास्ते से गुज़र रहा था। उसे तेज़ प्यास लगी। उसको एक कुँआ मिला। वह उसमें उतरा और उसने पानी पिया। फिर बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता अपनी जीभ निकाले हाँफ रहा है और (प्यास के मारे) गीली मिट्टी खा रहा है। वह व्यक्ति बोला कि इस कुत्ते का भी प्यास से वही हाल हो गया है जैसा कि मेरा हो गया था। फिर वह कुँए में उतरा और अपने मोज़े में पानी भरा। फिर अपने मुँह से मोज़े को थामकर वह ऊपर चढ़ा और उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ने उसकी इस नेकी को अभिस्वीकृति प्रदान की और उसे क्षमादान दिया।" लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जानवरों के सिलसिले में भी हमारे लिए प्रतिदान है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "प्रत्येक आर्द्र जिगर (कलेजे) में तुम्हारे लिए प्रतिदान है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : उस व्यक्ति ने देखा कि प्यास के कारण उस कुत्ते का बुरा हाल है। यहाँ तक कि प्यास की अधिकता से वह गीली मिट्टी चाट रहा है। चूँकि हाथ से कुँए की दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ना था इसलिए मोज़े को उसने दाँत से पकड़ लिया। कुत्ते पर उसका रहम खाना अल्लाह को इतना पसन्द आया कि उसके यहाँ उसकी यह नेकी स्वीकृत हो गई और यह नेकी उसकी मुक्ति का कारण सिद्ध हुई।
यह प्रश्न कि 'क्या जानवरों के सिलसिले में भी प्रतिदान है' का अर्थ यह है कि क्या जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने और उनपर दया करने में ईश्वर हमें सवाब (इनाम) देगा?
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन कि 'प्रत्येक आर्द्र जिगर में तुम्हारे लिए प्रतिदान है' बुनियादी महत्व रखता है। जिस किसी में चेतना और संवेदना पाई जाती है, चाहे वह जानवर और चौपाया ही क्यों न हो, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। उसे अकारण कष्ट पहुँचाना जायज़ नहीं है। उसपर दया करना अल्लाह को प्रिय है और इस पर वह लोगों को सवाब प्रदान करेगा।
(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “एक महिला नरक में एक बिल्ली के कारण डाली गई। उसने उसे बाँध रखा था। न तो उसने उसे कुछ खाने को दिया और न उसे छोड़ा कि वह (चल-फिरकर) भूमि के जीव-जन्तुओं में से कुछ खा लेती।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम की एक विस्तृत हदीस से यह मालूम होता है कि उस निर्दयी औरत ने उस बिल्ली को बाँधे रखा यहाँ तक कि वह इसी हाल में भूखी-प्यासी मर गई। इस हदीस से यह भी पता चलता है कि वह स्त्री बनी-इसराईल की थी।
यह हदीस बताती है कि निर्दयता और कठोरतापूर्ण व्यवहार इतना बड़ा अपराध है कि इसके कारण आदमी नरक जैसे परिणाम से भी दोचार हो सकता है। निर्दयतापूर्ण व्यवहार चाहे वह जानवरों के साथ ही क्यों न किया जाए, इस बात का प्रमाण है कि आदमी ईमान की वास्तविकता और उसकी अपेक्षाओं से बिलकुल अपरिचित है। उसे ईश्वर की पकड़ का भी भय नहीं है। वह नहीं सोचता कि जानवर जो उसके अधीन किए गए हैं उसकी अपेक्षा कमज़ोर और विवश तो हैं लेकिन वह ईश्वर जो हमारे समस्त कार्यों को देख रहा है, कदापि कमज़ोर या विवश नहीं है।
(3) हज़रत आमिर रामी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि उस समय हम उनके अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकट ही थे कि एक व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया। वह कम्बल ओढ़े हुए था। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसको उसने कम्बल से लपेट रखा था। उसने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं वृक्षों के झुंड के पास से गुज़रा। वहाँ मुझे चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने उन्हें पकड़ कर अपने कंबल में रख लिया, फिर उनकी माँ आई और मेरे सिर पर चक्कर लगाने लगी। मैंने बच्चों के ऊपर से कंबल उसके लिए हटा दिया। वह उनपर आ गिरी। मैंने उन सबको अपने कम्बल में लपेट लिया। अब वे सब मेरे पास हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— "उन्हें ज़मीन पर रख दो।” अतएव उसने उन्हें रख दिया। बच्चों की माँ ने उन बच्चों से लिपटे रहने के सिवा सब कुछ छोड़ दिया। इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "बच्चों की माँ के अपने बच्चों पर इस दया पर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। क़सम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, अल्लाह अपने बन्दों पर इससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है जितना इन बच्चों की माँ अपने बच्चों पर है। तुम इन्हें ले जाकर जहाँ से इनको इनकी माँ के साथ पकड़ा है वहीं रख दो।" अतः वह व्यक्ति उनको लेकर वापस चला गया। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : चिड़िया अपने बच्चों के प्रेम में विकल हो गई थी और उनके लिए उस व्यक्ति के ऊपर मँडराने लगी थी। जैसे ही उसके बच्चों पर से कम्बल हटाया गया और उसने बच्चों को देखा तो ममता की मारी माँ व्याकुल हो अपने बच्चों पर आ गिरी। फिर न तो वह अपनी जान बचाकर उड़ी और न कुछ और किया। उसने बच्चों को नहीं छोड़ा। प्रत्येक डर और ख़तरे से बेपरवाह होकर वह अपने बच्चों से चिमटी ही रही।
ईश्वर की रहमत अपने बन्दों के साथ उससे भी बढ़कर है जितना माँ अपने बच्चों पर मेहरबान होती है। फिर लोग हैं कि ऐसे मेहरबान ईश्वर के साथ नाता तोड़कर अपने लिए स्वयं ही तबाही और हलाकत का सामान करते हैं।
(4) हज़रत सहल-बिन-हनज़लिय्यह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसकी पीठ उसके पेट से लग गई थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इन बेज़बान जानवरों के सम्बन्ध में अल्लाह से डरो। इनपर ऐसी हालत में सवारी करो जबकि ये इसके योग्य और स्वस्थ हों और इन्हें इस हाल में छोड़ो कि ये अच्छी हालत में हों।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ऊँट बहुत दुर्बल और भूखा था। साफ़ महसूस हो रहा था कि उससे काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन उसके आराम और उसकी भूख-प्यास की कुछ भी परवाह नहीं की जाती। इस चीज़ ने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया था।
ये बेज़बान हैं, तुमसे कुछ कह नहीं सकते, न अपने मुँह से तुम्हें बुरा कह सकते हैं, और न किसी से तुम्हारी शिकायत कर सकते हैं।
इनपर रहम करो और इनके मामले में ईश्वर से डरते रहो। जब ये सवारी के योग्य हों तो इनसे सवारी का काम लो और इससे पहले कि ये थककर चूर हों और इनकी हालत ख़राब हो, इन्हें छोड़ दो कि इनकी शक्ति वापस आ जाए और ये कुछ खा-पी लें और आराम कर लें।
(5) इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस व्यक्ति पर लानत की है जो जानवरों का अंग-भंग करे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात उन के कान इत्यादि काटकर उनकी शक्ल-सूरत न बिगाड़ो। इससे ईश्वर का क्रोध भड़कता है और आदमी उसकी रहमतों से दूर हो जाता है।
(6) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुँह पर मारने और दाग़ने से मना किया है। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : शरीर में मुँह अत्यन्त नाज़ुक और संवेदनशील अंग है। उसपर मारने या उस पर दाग़ देने से जानवर को अत्यन्त कष्ट होता है। अकारण किसी जानवर को कष्ट देना निर्दयता और कठोरहृदयता की बात है, और मानवीय आचरण के अत्यन्त प्रतिकूल है।
(7) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा : "किसी प्राणधारी को निशाना न बनाओ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इसी प्रकार सहीह मुस्लिम की एक और हदीस में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जानवरों को बाँधकर मारने से मना किया है।
किसी जानवर को चाँदमारी के लिए इस्तेमाल करना या उसे बाँधकर मारना कि वह अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सके, अत्यन्त निर्दयता और कठोरता है। इस्लाम तो इसलिए आया है कि लोगों के दिलों से कठोरता और निर्दयता को दूर करे और उन्हें रहमत की प्रतिमूर्ति बना दे। निर्दयता और निष्ठुरता को, चाहे वह किसी रूप में हो, इस्लाम कभी भी पसन्द नहीं कर सकता।
(8) हज़रत शद्दाद-बिन-औस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कही हुई दो बातें याद रखी हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने हर काम में भलाई और अच्छाई को अनिवार्य किया है। जब क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो ओर जब ज़िब्ह करो तो अच्छे तरीक़े से ज़िब्ह करो। तुममें से जो कोई ज़िब्ह करना चाहे तो उसे चाहिए कि छुरी को तेज़ कर ले और अपने जानवर को (यथासम्भव) आराम पहुँचाए।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात भलाई और अच्छाई की किसी भी मामले में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए यहाँ तक कि अगर दुश्मन या किसी अपराधी को क़त्ल करना हो उसमें भी इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि उसे उत्पीड़ित कर या तड़पा-तड़पा कर न मारा जाए। और न उसके चेहरे को बिगाड़ा जाए। अगर जानवर को ज़िब्ह करना हो तो उसमें भी अच्छा ढंग अपनाना चाहिए, उदाहरणार्थ जानवर भूखा-प्यासा न हो, जिस छुरी से ज़िब्ह करना हो वह तेज़ हो। ताकि ज़िब्ह करने में आसानी हो और जानवर को कम से कम कष्ट पहुँचे। इसी प्रकार जानवर के सामने छुरी तेज़ न करें और न किसी जानवर के सामने किसी जानवर को ज़िब्ह करें, आदि।
अध्याय-2
सामाजिक गुण (दृष्टि एवं विवेक)
(1)
बुद्धिमत्ता और अल्लाह के लिए प्रेम
बुद्धिमत्ता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लोगों से उनके स्तर के अनुरूप व्यवहार करो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दर्जा और एक स्थान होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे उसके दर्जे पर रखें। न तो हम उसे वह दर्जा देने लग जाएँ जो उसे प्राप्त नहीं है और न उसकी उस हैसियत की उपेक्षा करें जो उसे प्राप्त है।
ज्ञान, ईशपरायणता और वैध विशिष्टताओं का ध्यान रखना आवश्यक है यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत-से भौतिकवादी क़िस्म के लोग मात्र धन को प्रतिष्ठा का मानदण्ड समझते हैं। यह सही नहीं है। एक ईश्वर के अवज्ञाकारी और मर्यादाहीन धनी व्यक्ति की अपेक्षा मान-सम्मान का अधिकारी वास्तव में वह निर्धन और धनहीन व्यक्ति है जो ईश्वर का आज्ञाकारी है या जिसे ईश्वर ने ज्ञान और श्रेष्ठता से सुशोभित किया है। दीन और परहेज़गारी की अपेक्षा सांसारिक धन-सम्पत्ति की कोई हैसियत नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वह है जो ईश्वर से डरनेवाला हो। सांसारिक धन-सम्पत्ति तो क़ारून के पास भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ईश्वर ने जब उसे उसकी अवज्ञा के कारण पकड़ा तो उसका धन उसके कुछ काम न आ सका। वह विनष्ट होकर रहा।
(2) हज़रत अबू-सईद अनसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नमाज़ के लिए (पंक्तियाँ सीधी करने के उद्देश्य से) हमारे कंधों पर हाथ फेरते और कहते—
“बराबर हो जाओ और विभेद पैदा न करो अन्यथा तुम्हारे दिल भी अलग-अलग हो जाएंगे। तुममें जो बुद्धि और समझवाले हैं वे मुझसे निकट रहें, फिर वे लोग जो उनसे निकट हैं और फिर वे लोग जो उन से निकट हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात नमाज़ में सीधे और बराबर खड़े हो। पंक्तियाँ टेढ़ी न हों अन्यथा तुम्हारे दिलों में भी फूट पड़ जाएगी। बाह्य अव्यवस्था और विसंगति आन्तरिक उपद्रव का लक्षण है। तुम्हारे अन्दर कोई फूट और विभेद न भी हो लेकिन अगर तुम बाह्य रूप से अव्यवस्थित रहोगे तो अनिवार्यतः इस का प्रभाव तुम्हारे अन्तर पर भी पड़ेगा और तुम्हारे दिल भी पृथक हो जाएँगे। फिर तुम्हारे अन्दर वह एकात्मता शेष न रहेगी जो धर्म में अभीष्ट है।
इस हदीस से ज्ञात हुआ कि बुद्धि और समझ का धर्म में बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जितनी अधिक समझ रखता है उतनी ही अधिक धार्मिक चेतना उसमें पाई जा सकती है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा ही इसके अधिक योग्य है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकट उसे स्थान मिले।
अल्लाह के लिए प्रेम
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अच्छा गुमान रखना अच्छी इबादत है।" (हदीस : अहमद, अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि सदाशा या अच्छा गुमान रखना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उत्तम इबादतों में से है। हमारी सदाशा का सबसे ज़्यादा हक़दार ईश्वर है। ईश्वर से अच्छी आशा न रखना इनसान के लिए केवल अभाग्य की बात नहीं है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी यह उसकी संवेदनहीनता, मानसिक गिरावट और असज्जनता का स्पष्ट प्रमाण है। जीवन में वास्तविक परीक्षा इसी बात की ली जा रही है कि हम अपने पालनकर्ता प्रभु से कैसी आशा रखते हैं। हमें उसपर और उसके वादों पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है या नहीं।
इनसानों और विशेषकर मोमिनों का यह भी हक़ होता है कि हम उनसे अच्छी आशा रखें। अकारण उन्हें बुरा जानना, कपटी, धूर्त और विश्वासघाती समझना और इसपर अड़े रहना एक सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमें न तो आचरण और नैतिकता के कोमल पक्षों का ज्ञान ही है और न ही कोई चिन्ता।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन प्रेम और आसक्ति का महल होता है। और उस व्यक्ति में कोई विशेषता और भलाई नहीं जो न स्वयं प्रेम करता है और न लोगों को उससे प्रेम होता है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अल-बैहक़ी)
व्याख्या : अर्थात मोमिन सर्वथा प्रेम और प्रेम का स्रोत होता है। लोगों से उसका वास्तविक सम्बन्ध प्रेम पर आधारित होता है। लोग भी उससे प्रेम करते हैं, और यह चीज़ बड़ी ख़ूबी और बरकत का कारण है। ईमानवालों की यह विशिष्टता अपने अन्दर एक प्रकार की क्रान्तिकारी शक्ति रखती है। यह क्रान्तिकारी शक्ति का ही करिशमा है कि प्रेम विश्व-विजयी होकर रहता है। इनसानों के दिल ईमानवालों की ओर झुकते हैं और अन्ततः एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जहाँ लोग एक-दूसरे के हमदर्द और दुख बाँटनेवाले होते हैं। फिर त्याग और प्रेम से परिपूर्ण वे आदर्श चरित्र सामने आते हैं जिनपर मानवता सदैव गर्व करती रहेगी।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम उस समय तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि ईमान न लाओ। और उस समय तक (सही अर्थों में) तुम मोमिन नहीं होगे जब तक कि आपस में एक-दूसरे से प्रेम न रखो। और क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बता दूँ कि जब तुम उसपर अमल करो तो तुम्हारे बीच प्रेम बढ़े। वह यह कि आपस में सलाम को प्रचलित करो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : सफल जीवन उसी व्यक्ति का है जो ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का पात्र हो। यह हदीस बताती है कि वही लोग स्वर्ग में जा सकेंगे जो ईमान लाएँगे, जिनकी नीति अवज्ञा और इनकार की न होगी। फिर ईमान स्वाभाविक रूप से हमसे कुछ बातों की माँग करता है। उनमें से एक यह है कि ईमानवाले आपस में एक-दूसरे से प्रेम रखें। ईर्ष्या-द्वेष और कपट और दंभ उनके दिलों में न रहे। ईमान के बाद भी अगर आदमी तंगदिल, तंगनज़र, साहसहीन, संकीर्ण और स्वार्थी ही बना रहा तो उस ईमान का क्या महत्व और मूल्य हो सकता है इसे आप स्वयं समझ सकते हैं।
एक-दूसरे को सलाम करने में एक बड़ी ख़ूबी है कि इसके बड़े प्रीतिकर प्रभाव इन्सान के दिल पर पड़ते हैं। लोगों में प्रेम और आसक्ति का सम्बन्ध पैदा होना, सलाम को रिवाज देना इसके लिए एक प्रभावी उपाय है।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! क़ियामत कब आएगी? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— “अफ़सोस तुझपर, तू ने उसके लिए क्या तैयारी की है?" उसने कहा कि मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तू उसी के साथ है जिससे तुझे प्रेम है।" हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का बयान है कि मैंने मुसलमानों को इस्लाम के बाद किसी चीज़ पर इतना प्रसन्न होते नहीं देखा जितना आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से वे प्रसन्न हुए। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि क़ियामत तो अपने समय पर आएगी ही, आवश्यकता है कर्म की। अनावश्यक प्रश्नों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए।
हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मेरे जो भी कर्म हैं उनको मैं कोई विशेष महत्व नहीं देता और न उनको उल्लेखनीय समझता हूँ। अलबत्ता मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम है। इसी का मेरी दृष्टि में महत्व है। वास्तव में मौलिक निर्णयात्मक चीज़ प्रेम ही है। वे सारे ही कर्म जिनका सम्बन्ध हृदय से है या शरीर और धन से, वास्तव में एक प्रेम ही की विभिन्न अभिव्यंजनाएँ हैं। प्रेम एक अत्यन्त कोमल और नाज़ुक भावना है। उसे ज़रा भी खोट गवारा नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम कार्यरत होगा वहाँ दिखावा, महत्वाकांक्षा, घमण्ड, अवज्ञा, उल्लंघन और इस प्रकार की दूसरी चीज़ों के पैदा होने की कोई सम्भावना शेष नहीं रहती।
प्रत्यक्ष कर्मों और नेक कामों की सूची तो लम्बी से लम्बी हो सकती है। आदमी कितने ही नेक काम अंजाम दे ले, फिर भी करने को कितने ही काम बाक़ी रह सकते हैं। कर्मक्षेत्र में दौड़-धूप की कोई सीमा नहीं। अगर प्रत्यक्ष कर्मों और प्रत्यक्ष नेकियों के आधार पर हमारे बारे में कोई निर्णय हो तो हमारे कर्म सीमित होंगे। ईश्वर की प्रसन्नता और उसका आत्यान्तिक सामीप्य हमारे हिस्से में कैसे आ सकेगा। चेतन या अचेतन रूप से आदमी को यह चिन्ता हो सकती है। लेकिन जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से सहाबा ने यह सुना कि तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम प्रेम रखते हो तो उन्हें असाधारण प्रसन्नता और आनन्द की अनुभूति हुई। इस्लाम की नेमत के बाद यह दूसरी बड़ी नेमत थी जो उनके हिस्से में आई। उन्होंने यह समझ लिया कि ईश्वर के यहाँ मूल निर्णायक चीज़ प्रेम और सद्भाव है। सद्भावना के प्रमाण के लिए दीर्घायु न अपेक्षित है और न अपरिहार्य।
(2)
सुरुचि
त्याग
(1) हज़रत सहल (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक महिला अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक बुना हुआ हाशियादार बुर्दा लेकर आई। क्या तुम जानते हो कि बुर्दा क्या चीज़ है? लोगों ने कहा कि शमला (चादर)। उन्होंने कहा कि हाँ। उस महिला ने कहा कि मैंने इसे अपने हाथ से बुना है। आई हूँ कि आपको पहना (ओढ़ा) दूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे क़बूल कर लिया। उस समय आपको उसकी आवश्यकता भी थी। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे पास आए। उस समय आपने उसे तहमद के तौर पर पहन रखा था। एक व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि इसे आप हमें प्रदान कर दें। यह कितनी अच्छी है। लोगों ने कहा कि यह तूने अच्छा नहीं किया। इसे तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आवश्यकतावश पहन रखा था और तूने इसे माँग लिया। हालाँकि तुझे मालूम है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किसी के सवाल को रद्द नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा कि अल्लाह की क़सम! इसे मैंने पहनने के लिए नहीं माँगा है बल्कि इसलिए माँगा है कि यही मेरा कफ़न हो। हज़रत सहल (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि वह चादर उसका कफ़न ही हुई। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किसी के सवाल को रद्द नहीं करते थे। उन्हें स्वयं चादर की आवश्यकता थी फिर भी चादर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने माँगनेवाले को दे दी। इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के त्याग से सम्बन्धित एक घटना का उल्लेख किया गया है। त्याग और उत्सर्ग वास्तव में नैतिकता और परोपकार का एक ऊँचा दर्जा है। त्याग यह है कि आदमी अपनी आवश्यकता की चिन्ता न करके दूसरे की आवश्यकता पूरी कर दे। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वयं अपना तरीक़ा त्याग का था और आप दूसरों को भी इसी पर उभारते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षा का यह प्रभाव था कि सहाबा के जीवन में हमें त्याग ही त्याग दिखाई देता है।
क़ुरआन ने भी अपने अनुयायियों को त्याग की शिक्षा दी है। अतएव कहा गया—
"और आपस में हक़ से बढ़कर देना न भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है जो कुछ तुम करते हो।" (2:237)
अनसार के त्याग और बलिदान की प्रशंसा में क़ुरआन में ये शब्द आए हैं—
“और वे अपने आप पर उन (मुहाजिर भाइयों) को प्राथमिकता देते हैं यद्यपि वे स्वयं अपनी जगह मुहताज ही हों।" (59:9)
उल्लेखों में हज़रत अबू-तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनकी पत्नी के त्याग की एक घटना का वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार अपने घर एक ज़रूरतमन्द को ले गए। घर में बच्चों के खाने के सिवा कुछ भी न था। बच्चों को बहलाकर सुला दिया जाता है। तदबीर से चिराग़ बुझा दिया जाता है। मेहमान समझता है कि खाने में वे भी शरीक हैं। सब खाना मेहमान ने खाया और उन्हें इसका एहसास भी न होने दिया कि घर के सभी लोग भूखे सोए हैं। सुबह को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें ख़ुशख़बरी दी कि अमुक बन्दे और बन्दी से अल्लाह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। हदीस में इसके लिए ‘अजिबल्लाहु’ या ‘ज़हिकल्लाहु’ के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द उपलक्ष्य या रूपक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
सीधी राह
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मध्यमार्ग अपनाओ और सन्मार्ग पर चलो।" (हदीस मुस्लिम)
व्याख्या : मध्यमार्ग अपनाओ अर्थात इबादत हो या कोई और काम, अतिवादिता से बचो। सन्तुलित व्यवहार ही सही अर्थों में हमारा आचरण या व्यक्तित्व बन सकता है। जो व्यवहार सन्तुलन से हटकर होगा उसपर हम देर तक क़ायम नहीं रह सकते। और अगर किसी प्रकार से हमने उसे निबाहने का प्रयास किया भी तो हमारा जीवन असन्तुलित होकर रहेगा, किसी एक तरफ़ को हम झुक जाएँगे। जीवन के कितने ही दूसरे महत्वपूर्ण दायित्वों को हम न निबाह सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे व्यक्तित्व में वह विशेषता और आकर्षण जो शरीअत में अभीष्ट है, शेष न रह सकेगा।
और यदि हम हद से आगे बढ़ने के बजाए हद से पीछे हट जाते हैं अर्थात आवश्यक सीमा तक भी दायित्वों को पूरा नहीं करते, इबादत से हमारा सम्बन्ध भी नाममात्र ही रहता है तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे जीवन में वे विशेषताएँ उत्पन्न न हो सकेंगी जो इबादतों और सत्कर्मों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती थीं। इसके अलावा हम इबादतों और अनिवार्य कार्य के करने में भी सुस्ती दिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, वह अनिवार्यतः कहीं न कहीं व्यय होगी। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम दोनों प्रकार की अति से बचकर सन्तुलित मार्ग अपनाएँ और जीवन में मध्यमार्ग के महत्व की कभी उपेक्षा न करें।
इस हदीस में सीधी राह अपनाने पर भी बल दिया गया है। सन्मार्ग मानव जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। सन्मार्ग या सीधा रास्ता अपनाना हमारा नैतिक और धार्मिक दायित्व ही नहीं बल्कि इसके बिना सही अर्थों में हम जीवन के वास्तविक अभिप्राय से परिचित भी नहीं हो सकते। सन्मार्ग की नीति आदमी को कितनी ही उलझनों और जटिलताओं से मुक्त करती है। सन्मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति और जीवन की मूल प्रकृति के मध्य एकात्मता पैदा हो सकती है और यही एकात्मता हमारे जीवित होने का प्रमाण है। अगर यह बात पैदा हो जाए तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अल्पायु भी पर्याप्त हो सकती है।
ईशपरायणता का जीवन
(1) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"वह व्यक्ति कामयाब हो गया जिस के दिल को ईश्वर ने ईमान के लिए विशिष्ट कर लिया और उसके दिल को भला-चंगा रखा, उसकी ज़बान को सच्ची और उसके आत्म को सन्तुष्ट बनाया। उसकी संरचना और प्रवृत्ति को सीधा रखा, उसके कान सुननेवाले बनाए और उसकी आँखें देखनेवाली बनाईं। अतः कान कीप हैं और आँख उसे क़ायम रखनेवाली है जिसको दिल सुरक्षित रखता है। और वह व्यक्ति कामयाब हो गया जिसके दिल को सुरक्षित रखनेवाला बनाया गया।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
व्याख्या : किसी आदमी के सफल होने की पहचान यह है कि उसका दिल ईमान और विश्वास से भरा हुआ हो। दिल ऐसा भला-चंगा हो कि उसमें कोई खोट न हो। कपटाचार और ईर्ष्या आदि से बिलकुल मुक्त हो। ज़बान का सच्चा हो। उसका अन्तर परितुष्ट अर्थात उसे अपने प्रभु का प्रेम और आज्ञापालन प्रिय हो। उसके स्वभाव और प्रवृत्ति में कोई टेढ़ न पाया जाए। न वह असत्य की ओर झुके और न वह किसी भी प्रकार की अतिवादिता में पड़े। फिर वह सत्य के सुनने और समझने की स्थिति में हो। उसे वह अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो कि ईश्वर के गुणों में वह ईश्वर की उपस्थिति और उसके एक होने के प्रमाणों को देख सकता हो। वह दुनिया में अन्धा-बहरा बनकर न रह रहा हो।
दिल पात्र के सदृश है और कान कीप के सदृश। जिस प्रकार कीप के द्वारा किसी शीशी या बोतल में हम तरल वस्तुओं को ढाल लेते हैं ठीक उसी प्रकार से कान के रास्ते सत्य हृदय में उतरता है। दिल जिन बातों को अपने अन्दर लेता है आँख उनको स्थायित्व प्रदान करती है। मोमिन की आँख दिल की सहायक और मददगार होती है। आँख सच्चाई से इनकार नहीं करती बल्कि वह बाह्य जगत् का आन्तरिक जगत् से सामंजस्य बिठाने में अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार दिल को सत्य के विषय में वह असन्दिग्धता और विश्वास प्राप्त होता है जो कभी डाँवाडोल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कान की तरह आँख के द्वारा भी दिल को सत्य की सूचना मिलती है।
जिस किसी व्यक्ति को सत्य की प्रतीति हो जाती है तो फिर वह न तो उसे भूल सकता है और न उसकी उपेक्षा कर सकता है। उस व्यक्ति के कामयाब होने में क्या सन्देह हो सकता है। दिल में अगर सत्य उतर चुका है और दिल ने उसे पूर्णरूपेण सुरक्षित कर लिया है तो इसका प्रभाव यह होगा कि मनुष्य अपने जीवन में सन्मार्ग से कभी विमुख नहीं हो सकता। उसका सम्पूर्ण जीवन सत्य और सत्यवादिता का दर्पण होगा। इस प्रकार दिल की दुरुस्ती इनसान की कामयाबी की वास्तविक ज़मानत है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सच कहा कि "वह व्यक्ति सफल हो गया जिसका दिल सुरक्षित रहनेवाला बना है।" क़ुरआन में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है—
"जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद सिवाय इसके कि कोई भला-चंगा दिल लिए हुए उसके पास आया हो।” (26: 88-89)
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ आइशा! उन गुनाहों से बचती रहना जिनको हल्का और साधारण समझा जाता है। इसलिए कि ईश्वर की ओर से उनके विषय में भी पूछा जाएगा।" (हदीस : इब्ने-माजा, दारमी, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : इससे ज्ञात हुआ कि छोटे गुनाहों से भी बचना आवश्यक है। मामूली गुनाह भी अगर कोई करता रहे तो इससे दिल को ज़ंग लग जाता है। बल्कि छोटे गुनाह पर आग्रह उसे बड़ा बना देता है। किसी गुनाह को छोटा समझकर इनसान का उसपर दिलेर होना सही नहीं है। इस सिलसिले में हाफ़िज़ इब्ने-क़य्यिम ने कितनी अच्छी बात कही है कि “गुनाह को यह न देखो कि वह कितना साधारण और छोटा है, बल्कि उस ईश्वर की महानता और बड़ाई को दृष्टि में रखो जिसकी अवज्ञा में दुस्साहस से काम लिया जा रहा है।" ईश्वर की महानता का एहसास अगर हो तो छोटे गुनाह भी गम्भीर प्रतीत होंगे।
(3) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा—
“तुम सुर्ख़ रंग के कारण बेहतर नहीं हो और न काले रंग के कारण से, बल्कि इनमें से प्रत्येक के साथ ईशपरायणता का होना भी आवश्यक है।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके रूप-रंग पर निर्भर नहीं करती बल्कि वास्तव में आदमी की श्रेष्ठता और उसकी विशेषता का सम्बन्ध ईश-भय से है। अर्थात इसका सम्बन्ध इससे है कि आदमी अपने जीवन में ईश्वर से कितना डरता है और वह सच्चाई का कितना लिहाज़ रखता है। आदमी के अन्दर जैसा ईशभय होगा उसी के अनुसार ईश्वर के यहाँ उसे स्थान प्राप्त होगा।
ईशभय का एक दर्जा तो यह है कि आदमी खुले बहुदेववाद से दूर रहे। यद्यपि अन्य मामलों में ईश्वर के आज्ञापालन का वह पूरा एहसास न रखता हो। ईशभय का एक दर्जा यह है कि आदमी ईश्वर का आज्ञाकारी हो और खुले बहुदेववाद से ही नहीं सूक्ष्म बहुदेववाद, उदाहरणार्थ दिखावा और महत्वाकांक्षा से भी बचता हो। लेकिन ईशभय का सर्वाधिक उच्च दर्जा यह है कि बन्दे को ईश्वर की उपस्थिति का सतत एवं जीवन्त एहसास हो। वह ईश्वर से किसी भी हाल में ग़ाफ़िल न रहे। उसके दिल में महानता हो तो ईश्वर की, ख़याल हो तो उसका, लगाव हो तो मूलतः उसी से, उसके दिल को चैन और आराम मिलता हो तो ईश्वर ही की याद से। और दिल उसका प्रत्येक प्रकार की निराधार शंकाओं से मुक्त हो।
लोगों के प्रति करुणा
(1) हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि सुफ़्फ़ावाले ग़रीब लोग थे। एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा—
"जिसके यहाँ दो आदमियों का खाना हो वह यहाँ से तीसरे को ले जाए और जिसके यहाँ चार आदमियों का खाना मौजूद हो तो वह पाँचवें या छटे को ले जाए।" अतएव (मेरे पिता) हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने साथ तीन आदमियों को ले आए। और स्वयं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने साथ दस व्यक्तियों को ले गए। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि अपने भाइयों को भूख की हालत में हरगिज़ न छोड़ो। जिसके पास दो आदमियों का खाना हो वह उसमें अपने तीसरे भाई को भी शरीक कर ले। इसी प्रकार जिसके घर चार आदमियों के लिए खाना उपलब्ध हो वह भी दो-एक व्यक्तियों को अपने साथ ले जाकर अपने खाने में शरीक कर ले।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने भूखों को खिलाने और उनपर दया दर्शाने ही की नसीहत नहीं की बल्कि स्वयं भी इसपर अमल किया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने व्यक्तिगत व्यवहार से इस बात का निर्देश दिया कि दूसरों की भूख और उनकी ज़रूरतों का हमें एहसास होना चाहिए और यथासम्भव लोगों की आवश्यकतापूर्ति को अपना धार्मिक दायित्व समझना चाहिए। विशेषकर एक ज़रूरतमन्द व्यक्ति के किसी ऐसे कष्ट की तो कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो आदमी के लिए असहनीय होती हो, उदाहरणार्थ, भूख-प्यास आदि।
शुभाकांक्षा
(1) हज़रत तमीम दारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“धर्म शुभाकांक्षा का नाम है।" यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार कहा। हमने निवेदन किया कि (यह शुभाकांक्षा) किसके लिए? कहा, "अल्लाह के लिए, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के इमामों और आम मुसलमानों के लिए।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस अत्यन्त संग्राहक हदीसों में से है। इस हदीस से धर्म के स्वभाव और उसकी व्यापकता का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। धर्म व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार के मामलों और समस्याओं में हमारा मार्गदर्शन करता है। वह एक ओर तो ईश्वर से हमारा सम्बन्ध सुदृढ़ करता है, दूसरी ओर वह ईश्वर के बन्दों के प्रति हमारे दायित्वों से हमें अवगत कराता है।
मूल में 'नसीहत' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका वास्तविक अर्थ है मिलावट और खोट से मुक्त होना। शहद को मोम इत्यादि से अलग करके उसे साफ़ कर लेते हैं तो उसे नसह्तुल-अस्ल कहते हैं। नुस्ह का सम्बन्ध मौखिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों से होता है। किसी को सही मश्विरा देने और उसका हित चाहने को भी 'नसीहत' कहते हैं। इसलिए कि विशुद्ध सम्बन्ध के लिए यह अपेक्षित है कि आदमी का जिस किसी से विशुद्ध सम्बन्ध और सम्पर्क हो उसे उसका दुष्चिन्तक कदापि न होना चाहिए बल्कि वह उसका हितैषी हो। आवश्यकता हो तो अपने अच्छे मश्विरों से उसे वंचित न रखे।
यह शुभाकांक्षा और विशुद्धता हर दशा में अभीष्ट है। यह धर्म में भी अपेक्षित है और इनसान के व्यक्तित्व का वास्तविक सौन्दर्य और गुण और उसकी ऊर्जा और शक्ति भी यही है। बहुत-से अनिवार्य कार्य और दायित्व विवशता की हालत में छोड़ दिए जाते हैं लेकिन शुभाकांक्षा की भावना प्रत्येक स्थिति में वांछित है। अतएव क़ुरआन में है—
“(जिहाद और दानशीलता के सम्बन्ध में) न तो कमज़ोरों के लिए कोई दोष की बात है और न बीमारों के लिए और न उन लोगों के लिए जिन्हें ख़र्च करने के लिए कुछ प्राप्त नहीं, जबकि वे अल्लाह और रसूल के शुभचिन्तक हों। उत्तमकारों पर इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह तो बड़ा क्षमाशील और दयावान है।" (क़ुरआन, 9:91)
ईश्वर के लिए नुस्ह (शुभाकांक्षा) का अर्थ यह है कि बन्दा अपने और अपने ईश्वर के बीच किसी प्रकार का खोट न रहने दे। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और वफ़ादारी में वह अत्यन्त निष्ठावान (Sincere) बनकर रहे। ईश्वर की किताब के लिए शुभाकांक्षा का अर्थ यह है कि उसके पाठ का हक़ अदा करे, उसकी आयतों में सोच-विचार और चिन्तन से काम ले। उसके प्रत्येक आदेश के आगे सिर झुका दे। सारे विश्व को उसकी ओर आमन्त्रित करे। हमारी सबसे बड़ी कामना यह हो कि ईश्वरीय पुस्तक के मार्गदर्शन में इन्सानों की वैचारिक और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो। इस पुस्तक के समस्त आदेश और नियम धरती में प्रचलित और लागू हों। यह पुस्तक अप्रभावी होकर कदापि न रहे।
ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हित चाहने और आपसे विशुद्ध सम्बन्ध का अर्थ यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम का सम्बन्ध सुदृढ़ हो। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मिशन को लेकर उठें। जिस सत्य धर्म को स्थापित करने के लिए आप दुनिया में आए थे उस धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया जाए और इसके लिए सिर-धड़ की बाज़ी लगा दी जाए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कार्यप्रणाली की तुलना में किसी दूसरी चीज़ को कदापि प्राथमिकता न दी जाए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन और कर्म की अपेक्षा किसी के विचार और कर्म को हरगिज़ प्राथमिकता न दी जाए।
मुसलमानों के इमामों (नेताओं और शासकों) या उनके प्रमुख व्यक्तियों का हित चाहने का अर्थ यह होता है कि भले कार्यों में उनसे सहयोग किया जाए। अतएव हदीस में है—
“श्रेष्ठ जिहाद उस व्यक्ति का है जिसने भ्रष्ट सत्ता के सामने हक़ बात कही।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)
इस नसीहत पर अमल का आदर्श इतिहास में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया। इब्ने-तैमिया ने मिस्र के दमनकारी सम्राटों के सामने और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने जहाँगीर के दरबार में इसी नसीहत पर अमल का आदर्श प्रस्तुत किया।
आम मुसलमानों का हित चाहने का अर्थ यह है कि अगर वे भटके हुए हों तो उनके सुधार की चिन्ता करे। उनमें धर्मज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करे। उन्हें कष्ट न पहुँचाए। उनके ऐबों को छिपाए। हितैषिता में उन्हें अपने समान जाने। उनमें से जिनपर अत्याचार हुआ हो उन्हें निस्सहाय न छोड़े। उनके सहायक बने। दुख-सुख में उनके साथ रहे। ज़रूरतमन्दों और निर्धनों की आवश्यकता पूरी करने में लापरवाही से काम न ले। उनको अपना भाई समझे और उन्हें अपना भाई समझकर उनसे व्यवहार करे। उनके साथ हमारा व्यवहार सहानुभूति और दर्दमन्दी का हो। क़ुरआन में है—
“मोमिन तो भाई-भाई ही हैं।” (49:10)
माता-पिता के सम्बन्ध से लोग भाई-भाई होते हैं। दीन और ईमान का रिश्ता तो सारे ही रिश्तों से गहरा और मज़बूत रिश्ता होता है। वह आख़िर लोगों को बन्धुत्व के रिश्ते में क्यों नहीं जोड़ सकता।
क़ुरआन के अध्ययन से पता चलता है कि नबियों के आमन्त्रण के पीछे वास्तव में सदाकांक्षा और हित चाहने की भावना ही कार्यरत रही है। अतएव हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) अपनी क़ौम से कहते हैं—
“मैं तुम्हें अपने रब के सन्देश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हित चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।" (7:63)
हज़रत हूद (अलैहिस्सलाम) ने भी अपनी क़ौम को सम्बोधित करते हुए यही कहा—
“मैं तुम्हें अपने रब के सन्देश पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा विश्वस्त हितैषी हूँ।” (7:68)
हज़रत सालेह (अलैहिस्सलाम) ने भी यही कहा था—
“ऐ मेरी क़ौम के लोगो! मैं तो तुम्हें अपने रब के सन्देश पहुँचा चुका और मैंने तुम्हारा हित चाहा। लेकिन तुम्हें अपने हितैषी पसन्द ही नहीं आते।" (7:79)
हज़रत शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने, जब क़ौम पर ईश्वर की ओर से यातना आई, तो उन्होंने यही कहा—
“ऐ मेरी क़ौम के लोगो! मैंने अपने रब के सन्देश तुम्हें पहुँचा दिए और मैंने तुम्हारा हित चाहा। अब मैं इनकार करनेवाले लोगों पर कैसे अफ़सोस करूँ!" (7:93)
(2) हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और प्रत्येक मुसलमान का हित चाहने पर बैअ्त की थी। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : हित चाहने के महत्व का अनुमान इससे किया जा सकता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नमाज़ और ज़कात के साथ इसपर भी बैअ्त ली है। शुभाकांक्षा की भावना अगर सही अर्थों में हमारे अन्दर पैदा हो जाए तो प्रत्येक प्रकार के दुराचारों और अनैतिकताओं का सर्वथा अन्त हो जाए। यह भावना उन समस्त बुराइयों को रोक देने के लिए पर्याप्त है जो आज हमारे समाज में सामान्यतः पाई जाती हैं। शुभाकांक्षा की भावना के साथ हम न किसी भाई की पीठ पीछे निन्दा कर सकते हैं और न उससे इर्ष्या कर सकते हैं और न ही उसके ऐबों का ढिंढोरा पीट सकते हैं। और न हम उसे किसी प्रकार की हानि पहुँचाना चाहेंगे बल्कि हमारा यह प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक अपने भाई के काम आ सकें। फिर तो हमारे अपने लिए प्रसन्नता और आनन्द की बात अपने भाई की प्रसन्नता और आनन्द से बढ़कर और कुछ न होगी। रिवायत में है कि हज़रत जरीर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक घोड़ा 300 दिरहम में ख़रीदा, फिर उन्होंने घोड़ा बेचनेवाले व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा का है, इसे 400 दिरहम में दोगे? उसने जवाब दिया कि ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम जानो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घोड़ा इससे अधिक मूल्यवान है। क्या तुम इसे 500 दिरहम में बेचोगे? वह इसी प्रकार मूल्य बढ़ाते गए और अन्ततः उन्होंने उसे 800 दिरहम में ख़रीद लिया। जब लोगों ने पूछा कि घोड़ा तो 300 दिरहम में मिल रहा था, आपने 800 दिरहम क्यों ख़र्च किए? तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रत्येक मुसलमान का हित चाहने पर बैअ्त कर रखी है।
इस घटना से अनुमान किया जा सकता है कि सहाबा एक-दूसरे के हितों का कितना ध्यान रखते थे।
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जो व्यक्ति यह पसन्द करता है कि उसे नरक से अत्यन्त दूर रखा जाए और स्वर्ग में प्रवेश करा दिया जाए तो चाहिए कि उसको मौत इस हाल में आए कि ईश्वर और अन्तिम दिन पर वह ईमान रखता हो और लोगों के साथ उसे वही मामला करना चाहिए जो वह चाहता है कि लोग उसके साथ करें।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात नरक की यातना से सुरक्षित रहने और स्वर्ग में स्थान पाने के लिए जिस प्रकार यह आवश्यक है कि आदमी मोमिन हो, वह ईश्वर और परलोक का इनकार न करता हो, उसी प्रकार उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसका शील-स्वभाव और चरित्र भी मोमिन का हो। अगर उसका स्वभाव और चरित्र मोमिन का नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि उसका ईमान इतना बेजान और कमज़ोर है कि उसके जीवन पर उसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात दुनिया के जीवन में उसका ईमान लाभदायक और प्रेरणा शक्ति न बन सका फिर ऐसे ईमान के द्वारा अगर हम बड़ी-बड़ी आशाएँ और उम्मीदें रखते हैं तो इसे बेसमझी और बेख़बरी के सिवा और क्या कहा जा सकता है!
जीवन में किसी के सुशील और चरित्रवान होने की इससे बेहतर कसौटी सम्भवतः दूसरी न हो कि आदमी स्वयं दूसरे लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करे जिस तरह वह चाहता है कि लोग उसके साथ व्यवहार करें। अर्थात अपने समान ही दूसरे लोगों की मान-मर्यादा और उनकी भलाई और उनकी सफलता भी उसे प्रिय हो।
भाई की सहायता एवं समर्थन
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने भाई की मदद करो चाहे वह अत्याचारी हो या उसपर अत्याचार हुआ हो।” एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जिसपर अत्याचार हुआ हो उसकी सहायता तो मैं करता हूँ, लेकिन अत्याचारी की सहायता कैसे करूँ? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “तुम उसे अत्याचार करने से रोको। बस यही (अत्याचार से उसको रोकना) तुम्हारा उसकी मदद करना है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : सम्भव है कि वह अत्याचारी व्यक्ति इसे अपनी मदद न समझे बल्कि इसे अनुचित हस्तक्षेप समझे लेकिन सत्य यह है कि यह उसकी सबसे बड़ी सहायता है कि तुम उसे अत्याचार और बुराई से बचा लो।
इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार करता है तो वास्तव में वह उस समय अपनी तुच्छ इच्छा और शैतान के अधीन होता है। उसे अत्याचार से रोकने का प्रयास शैतान और तुच्छ इच्छाओं के मुक़ाबले में उसकी सहायता करना है।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह अल-ख़ुतमी से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिस समय सेना भेजने का इरादा करते तो कहते—
“मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारी अमानत और तुम्हारे कर्मों के परिणाम को ईश्वर को सौंपता हूँ।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : एक और रिवायत में है कि हज़रत क़ज़आ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि मुझसे इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा—
“आओ मैं तुम्हें इस प्रकार विदा करूँ जैसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझे विदा किया था। मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारी अमानत और तुम्हारे कार्य सम्बन्धी परिणाम को ईश्वर को सौंपता हूँ।”
इन उल्लेखों से मालूम होता है कि आदर्श पारस्परिक सम्बन्ध और सम्पर्क यह है कि लोग एक-दूसरे के सहायक और संरक्षक हों। यह संरक्षण केवल एक-दूसरे की जान-माल और प्रतिष्ठा तक ही न हो बल्कि लोग एक-दूसरे के धर्म और नैतिकता और चरित्र के भी रक्षक हों। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चूँकि ईश्वर के रसूल थे इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को लोगों के धर्म और नैतिकता की सुरक्षा की सबसे अधिक चिन्ता रहती थी। इसका अन्दाज़ा उन हदीसों से भली-भाँति किया जा सकता है जिन्हें यहाँ उद्धृत किया गया है।
“मैं तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे कार्य सम्बन्धी परिणाम को ईश्वर को सौंपता हूँ।” का अर्थ यह है कि अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मेरे निकट थे तो मैं तुम्हारा रक्षक था लेकिन दूरी के कारण अब यह सम्भव न हो सकेगा। लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। वह तुम्हें धर्म से विमुख होने से बचाएगा और जिस प्रकार आज तुमपर भरोसा किया जाता है और तुम विश्वासपात्र हो, उस विश्वास को वही बनाए रखेगा और उसे क्षतिग्रस्त होने से वही बचाएगा। तुम्हारे जितने भी नेक कर्म हैं, जो तुम्हारे शील-स्वभाव को उजागर करते हैं, उनमें से किसी कर्म से तुम न फिरो, तुम अपनी सुचरित्रता को अन्त तक बनाए रख सको, वह तुम्हें इसकी सामर्थ्य प्रदान करेगा।
यहाँ यह ध्यान रहे कि अमानत का वास्तविक अर्थ वह नहीं है जिस अर्थ में यह शब्द हमारे यहाँ प्रयुक्त होता है। हमारे यहाँ उस वस्तु को अमानत कहते हैं जिसको सुरक्षा के उद्देश्य से किसी के पास रखा जाता है। इसे तो अरबी में वदीअत कहते हैं। अमानत का मूल अर्थ है ‘विश्वासपात्र होना।' उदाहरणार्थ लोग निश्चिन्त हों कि अमुक व्यक्ति हमारा हक़ हरगिज़ नहीं मारेगा। क़ुरआन में है—
“फिर अगर तुममें से एक-दूसरे पर भरोसा करे तो जिस पर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वह यह सच कर दिखाए कि वह विश्वासपात्र है और अल्लाह का, जो उसका रब है, डर रखे।" (2:283)
अर्थात जिस व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा किया गया है वह उस विश्वास और भरोसे को आघात न पहुँचने दे।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी व्यक्ति के सामने उसके मुसलमान भाई की ग़ीबत की जाए और वह उस मुसलमान भाई की सहायता की सामर्थ्य रखता हो और उसने उसकी मदद की तो अल्लाह दुनिया और आख़िरत में उसकी मदद फ़रमाएगा और अगर उसने उसकी मदद न की जबकि उसे उसकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त थी तो अल्लाह उसे इस कारण दुनिया और आख़िरत में पकड़ेगा।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : अर्थात किसी भाई की ग़ीबत हो रही हो तो चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि प्रतिरक्षा का पूरा प्रयास करना चाहिए। अतएव एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति ने अपने भाई के माँस की उसकी अनुपस्थिति में रक्षा की तो ईश्वर पर अनिवार्य है कि उसे नरक की अग्नि से मुक्त करे।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
अर्थ यह है कि अगर वह लोगों को भाई की निन्दा करने से रोकेगा और उन्हें इस अशोभनीय कर्म से दूर रखेगा तो ईश्वर उसे नरक से मुक्त करेगा। माँस की प्रतिरक्षा से अभिप्राय भाई के माँस को खाने से रोकना और मना करना है। यह संकेत पीठ पीछे उसकी निन्दा की ओर है। जैसा कि क़ुरआन में है—
“क्या तुममें से कोई पसन्द करेगा कि वह अपने मुर्दा भाई का माँस खाए?" (49:12)
पीठ पीछे निन्दा की उपमा मृत भाई का माँस खाने से दी गई है। ग़ीबत करके कोई चूँकि अपने भाई की प्रतिष्ठा का हनन करता और उसकी एक प्रकार से हत्या करता और उसे चरित्रहीन और मुर्दार ठहराता है, इसलिए यह उपमा अत्यन्त अर्थपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चूँकि उपस्थित न होने के कारण जिसकी ग़ीबत की जाती है वह अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता, इस दृष्टि से भी उसका माँस खाना मुर्दा भाई का माँस खाना है क्योंकि मुर्दा व्यक्ति कभी अपनी प्रतिरक्षा में समर्थ नहीं होता। इस उपमा से ग़ीबत का घिनावनापन भी पूर्णतः उजागर हो जाता है।
(4) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो मुस्लिम व्यक्ति उस मौक़े पर मुस्लिम व्यक्ति की सहायता न करे जहाँ उसका अनादर किया जाता हो और जहाँ उसकी आबरू को आघात पहुँचाया जाता हो तो अनिवार्यतः अल्लाह उसकी उस अवसर पर मदद न करेगा जहाँ उसे उसकी मदद की चाहत होगी। और जो कोई मुस्लिम व्यक्ति उस अवसर पर मुस्लिम व्यक्ति की मदद करे जहाँ उसकी आबरू को आघात पहुँचाया जाता हो और जहाँ उसका अनादर हो रहा हो तो अनिवार्यतः अल्लाह उसकी उस अवसर पर सहायता करेगा जहाँ उसे उसकी सहायता की चाहत होगी।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से स्पष्टतः प्रकट होता है कि कोई आदमी जैसे आचरण का होगा, ईश्वर उसी के अनुसार उसके साथ मामला करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मुसलमान भाई की मदद नहीं करता, हालाँकि मामला भाई की प्रतिष्ठा और मर्यादा का है, तो वास्तव में वह स्वयं को ईश्वर की सहायता से वंचित कर रहा है। ईश्वर भी उस समय उसकी सहायता से अपना हाथ खींच लेगा जबकि उसे मदद की बड़ी आवश्यकता होगी।
सत्य यह है कि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति ईश्वर की अमान में होता है इसलिए उसकी जान, उसका माल और उसकी आबरू की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। इस दायित्व की उपेक्षा जघन्य अपराध है। इस अपराध के दण्ड से उसे कोई भी न बचा सकेगा।
वचनबद्धता
(1) हज़रत उबैदुल्लाह-बिन-अब्दुल्लाह से उल्लिखित है कि उन्हें अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़बर दी कि उनको अबू-सुफ़ियान ने बताया कि हिरक़्ल ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि वह नबी तुम्हें किस बात का आदेश देता है तो तुमने कहा कि वह “नमाज़, सच्चाई, पाकदामनी, वचन का पालन और अमानतों की अदायगी का आदेश देता है।" उसने (हिरक़्ल ने) कहा कि "यह तो नबी का गुण है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इस हदीस में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह उस समय घटित हुई थी जब अबू-सुफ़ियान ईमान नहीं लाए थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हिरक़्ल (क़ैसरे-रूम) को पत्र लिखा था जिसमें उसको सत्य-धर्म स्वीकार करने का आमन्त्रण दिया गया था। अबू-सुफ़ियान क़ुरैश के उन कुछ सवारों के साथ बैठे हुए थे जो सीरिया में सौदागरों की हैसियत से गए थे। उस समय ये लोग एलिया में थे। हिरक़्ल ने उन लोगों के पास अपना आदमी भेजा और उन्हें दरबार में बुलवाया और कहा कि तुममें से कौन वंशावली की दृष्टि से उस व्यक्ति से ज़्यादा निकट है जिसने अपने नबी होने का दावा किया है। अबू-सुफ़ियान ने कहा कि मैं इन सबसे अधिक रिश्ते में उससे निकट हूँ। हिरक़्ल ने कहा कि अबू-सुफ़ियान को मेरे निकट कर दो और उनके साथियों को पीछे रखो। हिरक़्ल के चातुर्दिक रोम (रूम) के गणमान्य लोग बैठे हुए थे। द्विभाषिया बुलाया गया। हिरक़्ल ने कहा कि मैं अबू-सुफ़ियान से उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न करूँगा जिसने नबी होने का दावा किया है। अगर ये ग़लतबयानी से काम ले तो तुम लोग फ़ौरन टोकना और उसका खंडन करना। इस अवसर पर हिरक़्ल ने अबू-सुफ़ियान से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आपके आन्दोलन के बारे में विभिन्न प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न उसका वह था जिसका उल्लेख इस हदीस में किया गया है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाओं को सुनकर हिरक़्ल के विवेक और उसकी अन्तर्दृष्टि ने पा लिया कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सच्चे नबी हैं। वह स्पष्टतः कहता है कि ये शिक्षाएँ तो वस्तुतः नबी ही की शिक्षाएँ हो सकती हैं। नबी की शिक्षाएँ ऐसी ही पवित्र होती हैं। वह एक ओर लोगों को ईश्वर की उपासना की ओर बुलाता है और दूसरी ओर वह लोगों के जीवन को पवित्र और स्वच्छ देखने का इच्छुक होता है। वह चाहता है कि लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हो। वे विश्वासपात्र, सच्चे और वचनबद्ध हों। झूठ और वचनभंग से उनका जीवन सर्वथा मुक्त हो।
(2) हज़रत अबू-जरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“नेकी कोई भी हो उसे तुच्छ न समझो। और अपने भाई से ऐसा वादा न करो कि उसे पूरा न कर सको।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : दृष्टिवानों की नज़र में प्रत्येक नेकी महत्वपूर्ण होती है। अपने परिणाम और प्रभाव की दृष्टि से छोटी नेकी भी छोटी नहीं होती। इसके अतिरिक्त बड़ी नेकियों की तरह छोटी नेकी का सम्बन्ध भी जीवन के महान मूल्यों से होता है। किसी नेक काम को तुच्छ समझना वास्तव में जीवन-मूल्यों को तुच्छ समझना है। हमें सोचना चाहिए कि एक नेक काम जिसे हम मामूली समझते हैं वह आदमी के मोमिन ही नहीं, उसके महान होने का भी प्रमाण हो सकता है, जिस प्रकार कि एक बुराई जिसको लोग हलकी समझकर नज़रअंदाज़ कर जाते हैं, कभी आदमी के चरित्रहीन, दुराचारी और अधम होने का प्रमाण होती है।
फिर तुम्हें अपने दायित्वों का पूरा बोध होना चाहिए। किसी से वादा करो तो यह सोचकर करो कि उसे हर क़ीमत पर पूरा करना है। अपने वादे को साधारण बात न समझो। ये वादा तुम्हारे अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए तुम्हारी पहचान बनता है। वादा तोड़ने का अर्थ केवल यही नहीं होता कि तुमने एक वादा किया जो पूरा न हो सका, बल्कि इससे साफ़ प्रकट होता है कि तुम जीवन के अर्थ से पूर्णतः अनभिज्ञ हो। मानवता, सज्जनता और मानवता के अभीष्ट दर्जे से दूर होने के बावजूद तुम्हें इसकी कुछ भी ख़बर नहीं कि तुमने अपने इस व्यवहार से क्या खोया और क्या पाया।
(3) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वादा भी एक क़र्ज़ (ऋण) है।" (हदीस : अत-तबरानी फ़िल-औसत)
व्याख्या : अर्थात तुम जिस प्रकार क़र्ज़ चुकाने को आवश्यक समझते हो, वादा निभाने को भी आवश्यक समझो। क़र्ज़ अदा करने की स्थिति में होकर भी अगर कोई क़र्ज़ के रुपये नहीं लौटाता तो दुनिया उसे नीच और बेईमान समझती है। फिर आख़िर वह कौन-सा तर्क है जिसकी दृष्टि से वचनभंग के बाद उसकी प्रतिष्ठा और ईमान को कोई आघात नहीं पहुँचता।
(4) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने भाई से हुज्जत न करो और न उससे मज़ाक़ करो और न उसे वचन देकर वचन-भंग करो।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में हुज्जत से अभिप्रेत ऐसी बहस या शास्त्रार्थ है जिसमें आदमी पहले ही से यह तय कर लेता है कि हमें अपनी बात पर अड़े रहना है। दूसरे की बात चाहे कितनी ही सत्य क्यों न हो उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना है।
मज़ाक़ से अभिप्राय ऐसा मज़ाक़ है जो शिष्टतापूर्ण हास्य-विनोद के रूप में न हो बल्कि जिसका उद्देश्य दूसरे को दुख पहुँचाना हो।
(5) हज़रत ज़ैद-बिन-अरक़म (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस समय आदमी अपने भाई से वादा करे और उसकी नीयत यह हो कि वह उसे पूरा करेगा, और किसी कारणवश वह उसे पूरा न कर सके और वादे पर न आए तो उसपर कोई गुनाह नहीं।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात अगर किसी उचित कारण से कोई व्यक्ति अपने वादे पर न आ सका तो वह अल्लाह की दृष्टि में गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर उसकी नीयत ही अपने वादे को पूरा करने की न रही हो। या उसे वादे के महत्व और दूसरे की परेशानियों की कोई चिन्ता ही न हो और मात्र सुस्ती के कारण वह अपने वादे को पूरा न कर सका तो उसके गुनहगार होने में सन्देह नहीं रहता।
सद्व्यवहार
(1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह उस व्यक्ति पर रहम करे जो नर्मी और उदारता से काम लेता है जबकि वह बेचता है और जबकि वह ख़रीदता है और जबकि वह तक़ाज़ा करता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नर्मी और उदारता से काम लेनेवाले के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दिल से दुआ निकली है। इससे इस बात का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि जीवन में उदारतापूर्ण व्यवहार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कितना प्रिय था।
(2) हज़रत अबू-क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“जिस किसी ने तंगदस्त को मोहलत दी या अपना हक़ जो उसपर था, माफ़ कर दिया तो अल्लाह क़ियामत के दिन की सख़्तियों से उसे मुक्ति देगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर को उसका यह कर्म इतना प्रिय है कि इसके बदले में वह उसे क़ियामत की सख़्तियों और परेशानियों से सुरक्षित रखेगा। उसने दुनिया में उसके साथ जिससे उसका मामला पेश आया नर्मी से काम लिया था, उसने उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया था इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि ईश्वर भी उसके लिए सख़्ती को पसन्द नहीं करेगा।
(3) हज़रत अबुल-यसर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते सुना—
“जो व्यक्ति (अपना हक़ वसूल करने मे) तंगदस्त को मोहलत दे या अपना हक़ माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे (क़ियामत के दिन) अपनी छाया में स्थान देगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात क़ियामत के दिन उसे सुख-चैन प्रदान करेगा।
मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा और हाकिम की रिवायत से मालूम होता है कि जितने दिन की कोई किसी निर्धन को मोहलत देता है उसे उतने दिन तक प्रत्येक दिन ऋण देते रहने का सवाब मिलेगा और अदायगी के नियत समय के समाप्त हो जाने पर यदि वह फिर मोहलत दे देता है तो उसे दिए हुए ऋण का दो गुना ऋण प्रत्येक दिन देते रहने का सवाब मिलेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईश्वरीय अनुकम्पा बहाना ढूँढती है।
(4) हज़रत अबू-राफ़े (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक जवान ऊँट क़र्ज़ लिया। फिर सदक़े के ऊँट आए तो अबू-राफ़े (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि आपने मुझे आदेश दिया कि मैं एक जवान ऊँट उस कर्ज़ देनेवाले को दे दूँ। मैंने निवेदन किया कि मैं तो (उसके ऊँट से) अच्छा ही ऊँट पा रहा हूँ कि सातवें बरस में दाख़िल है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “वही उसको दे दो। क्योंकि लोगों में अच्छा व्यक्ति वही है जो चुकाने में उनमें सबसे अच्छा हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मैं इस ऊँट को कैसे दे दूँ। यह ऊँट तो उससे अच्छा है जो उसने कर्ज़ में दिया था। कर्ज़ में जो ऊँट उसने दिया था उस तरह का ऊँट मौजूद नहीं है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन का अभिप्राय यह है कि तुम इसकी बिलकुल परवाह न करो कि क़र्ज़ देनेवाले के ऊँट से अच्छा ऊँट तुम उसे दे रहे हो। भौतिक लाभ से कहीं अधिक लाभप्रद बात यह है कि तुम ईश्वर की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति ठहरो।
आपसी मेलजोल
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मोमिन प्रेम और सौहार्द की प्रतिमूर्ति होता है। और उस व्यक्ति में कोई भलाई नहीं जो न किसी से प्रेम रखता है और न किसी को उससे प्रेम होता है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : जिस समाज में लोगों के बीच प्रेम और आत्मीयता के स्तर पर परस्पर सम्बन्ध पैदा न हो वह कभी आदर्श समाज नहीं बन सकता। इसी लिए इस्लाम ने आपसी मेलजोल और प्रेम और आत्मीयता पर बहुत बल दिया है। लोगों के दिल परस्पर मिले हुए हों। क़ुरआन इस चीज़ को लोगों के लिए बड़ी नेमत (ईश-अनुग्रह) क़रार देता है। कहा गया है—
“और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुमपर हुई। जब तुम आपस में एक-दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम भाई-भाई बन गए।” (3:103)
उस व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं अपने लिए भी और इस धरती के लिए भी एक बोझ है जो प्रेम और अनुराग की बहुमूल्य निधि के महत्व और उसके आनन्द से अपरिचित है। जो व्यक्ति लोगों से प्रेम नहीं रखता और न उससे किसी को कोई रुचि और लगाव होता है, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ऐसा व्यक्ति अशुभ और लोगों की दृष्टि में अत्यन्त अभागा और मनहूस होता है।
(2) यह्या बिन-वस्साब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के एक बड़े सहाबी के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति लोगों से मिलता-जुलता और उनकी दुख देनेवाली बातों पर सब्र करता है वह उस व्यक्ति से अच्छा है जो लोगों से न तो मिलता-जुलता है और न उनकी दुख देनेवाली बातों पर सब्र से काम लेता है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : लोगों से सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित करने में और उसे बाक़ी रखने में निश्चय ही कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं और लोगों की ओर से कष्टदायक बातें भी सुननी पड़ती हैं। इसलिए कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। अब अगर कोई इन समस्त बाधाओं और ख़राबियों के बावजूद लोगों से कटकर नहीं रहता और उनसे सम्बन्ध और सम्पर्क बनाए रखता है और इस सिलसिले में जो कष्ट और दुख भी उसे पहुँचते हैं वह उन्हें सहन करता है तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में उससे बेहतर है जो न लोगों से मिलता है और न लोगों की दुखदायक बातों पर सब्र से काम लेता है। केवल अपनी सुरक्षा की चिन्ता एक प्रकार की स्वार्थपरता है जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता।
परस्पर सुलह कराना
(1) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या मैं तुम्हे न बताऊँ कि रोज़ा, सद्क़ा और नमाज़ से भी दर्जे में श्रेष्ठ चीज़ क्या है?" हमने कहा कि क्यों नहीं, आप अवश्य बताएँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह है परस्पर एक-दूसरे के बीच सुलह कराना। और परस्पर एक-दूसरे के बीच बिगाड़ पैदा करना वह अपकर्म है जो (समस्त नेकियों को) मूंड देनेवाला है।” (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में आदमी अपेक्षित मानदण्ड पर पूरा उतर सके तो यह इस बात की पहचान होगी कि सत्य-धर्म उसका चरित्र बन चुका है। व्यावहारिक जीवन में जब तक वह अपने ईश्वरवादी होने का सुबूत नहीं देता यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म उसका चरित्र बन सका है। सम्भव है कि एक व्यक्ति देखने में तो रोज़ा और नमाज़ आदि की पाबन्दी करता हो लेकिन चरित्र और व्यक्तित्व की दृष्टि से भरोसे के योग्य वह न हो। इसी लिए हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) आदमी के अच्छे होने के लिए यह आवश्यक समझते थे कि वह चरित्र, व्यक्तित्व और व्यवहार में भी अच्छा साबित हो। केवल किसी की नमाज़ देखकर उसके अच्छे होने का फ़ैसला करने को वे सही नहीं समझते थे। अगर एक व्यक्ति लोगों के बीच सुधार कार्य के लिए प्रयासरत हो तो उसका यह कार्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह व्यक्ति चरित्रवान है। इस दृष्टि से रोज़ा और नमाज़ और सदक़ा आदि की अपेक्षा उसके इस कर्म को विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त नमाज़ और रोज़ा और सद्क़े के असल फ़ायदों और उसकी बरकतों का सम्बन्ध विशेष रूप से आदमी के अपने आत्म से होता है जबकि सुधार कार्य और उपद्रवों की रोकथाम के अच्छे परिणामों से पूरा समाज लाभान्वित होता है।
इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सुधार कार्य से इबादत और आज्ञापालन के लिए रास्ते सुगम होते हैं और उसके द्वारा सारे दुर्भाग्यों का निवारण हो जाता है।
धर्म में परस्पर सुलह और सुधार कराने का महत्व इतना अधिक है कि इस सम्बन्ध में हितकर झूठ से काम लेने में कुछ हर्ज नहीं समझा गया है। अतएव हदीस में है—
“झूठ केवल तीन अवसरों पर वैध है, मर्द का अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए झूठ बोलना, युद्ध में झूठ बोलना और लोगों के बीच सुलह कराने के ध्येय से झूठ बोलना।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा :
“वह व्यक्ति झूठा नहीं है जो लोगों के बीच सुधार करे, भली बात कहे और नेक बात पहुँचाए।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
अर्थात ऐसी बात कहे कि जो बनाव और सुलह में सहायक हो और एक की ओर से दूसरे से वह बात कहे जिससे उसकी नाराज़ी दूर हो सके और वे परस्पर एक-दूसरे से निकट हो सकें।
(हदीस की किताब) मुस्लिम में है कि उम्मे-कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने कहा— "मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नहीं सुना कि उन मामलों में से किसी में छूट दी हो जिनको लोग झूठ क़रार देते हैं सिवाय तीन बातों में— युद्ध में, लोगों के बीच सुलह कराने में और मर्द के अपनी बीवी से बात करने में और औरत के अपने पति से बात करने में।"
इससे मालूम हुआ कि यह छूट केवल मर्द ही के लिए नहीं है, बल्कि औरत भी इससे फ़ायदा उठा सकती है।
युद्ध के अवसर पर यदि शत्रु पर अपना प्रभाव डालने के लिए यह घोषणा कर दी जाए कि हमारी सहायता के लिए सेना की एक ताज़ा दम टुकड़ी आ रही है। हालाँकि सहायता के लिए कोई सेना वहाँ पहुँचनेवाली न हो तो इसमें कोई दोष नहीं। यह जंगी चालों में से एक चाल है।
जनसेवा
(1) हज़रत सहल-बिन-साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ौम का सरदार सफ़र में लोगों का सेवक होता है। अतः जो व्यक्ति सेवा करके उनसे अग्रसर हो जाए उससे कोई व्यक्ति किसी भी कर्म के द्वारा बाज़ी नहीं ले जा सकता सिवाय इसके कि शहीद होने का स्थान उसे प्राप्त हो।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
व्याख्या : अर्थात सरदार वास्तव में लोगों से सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए होता है। उसको बड़ाई और बुज़ुर्गी लोगों की सेवा के कारण प्राप्त होती है। क़ौम के सरदार या प्रमुख का दायित्व है कि वह लागों की आवश्यकताओं को समझे और उनके लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करे। क़ौम में जो लोग बे सहारा और मजबूर और कमज़ोर हों उनकी सहायता, सेवा और सहयोग करे। सफ़र में चूँकि ज़्यादा कठिनाइयों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है इसलिए सफ़र का ज़िक्र किया गया। सफ़र में सरदार का दायित्व और भी बढ़ जाता है।
कुछ विद्वानों ने इस हदीस का अर्थ यह समझा है कि वास्तव में क़ौम का प्रमुख वह है जो क़ौम की सेवा करता हो चाहे देखने में प्रतिष्ठित लोगों में उसकी गणना न होती हो जैसा कि ‘फ़मन स-ब-क़-हुम बिख़िदमतिन’ अर्थात “जो सेवा के कारण लोगों से आगे बढ़ जाए" से ज्ञात होता है कि कोई भी कर्म सेवा से बढ़कर नहीं हो सकता।
आवश्यकतापूर्ति, सहायता और कार्य-साधना ईश्वरीय गुण है। क्योंकि जनसेवा को ईश्वरीय स्वभाव से एक प्रकार की सदृशता प्राप्त है इसलिए उसकी श्रेष्ठता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। अलबत्ता शहीद चूँकि ईश्वरीय मार्ग में हक़ और न्याय के लिए कष्ट ही नहीं उठाता बल्कि अपने प्राण भी न्योछावर कर देता है, इसलिए उसके उच्च स्थान से किसी को इनकार नहीं हो सकता।
नाते-रिश्ते का आदर
(1) हज़रत अम्र-बिन-अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल ने कहा—
“मुझे अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ने और बुतों को तोड़ने के लिए भेजा है कि हम ईश्वर को अकेला ईश्वर मानें और किसी भी चीज़ को उसका साझी न ठहराएँ।" यह बात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस समय कही जबकि उल्लेखकर्ता ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा था कि अल्लाह ने आपको किस कार्य के लिए भेजा है। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत अम्र-बिन-अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस्लाम के अत्यन्त प्रारम्भिक चरण में मक्का आए थे और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित होकर पूछा था कि आप कौन हैं? इस अवसर पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि मैं पैग़म्बर हूँ। उन्होंने पूछा कि पैग़म्बर किसे कहते हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है। अम्र-बिन-अबसा ने पूछा कि किस लिए भेजा है? इस सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वह बात कही जो इस हदीस में वर्णित हुई है।
इसके बाद अम्र-बिन-अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने पूछा कि किन लोगों ने आपका साथ दिया है? कहा कि एक स्वतन्त्र और एक दास ने। यह इशारा हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) की और था। उन्होंने कहा कि मैं भी आप का साथ देता हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि इस समय अपने घर लौट जाओ, जब मेरे विजय की सूचना मिले तो आ जाना।
इस हदीस में तौहीद के साथ रिश्ते-नाते को जोड़ने को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने नबी होने का उद्देश्य क़रार दिया है। इससे नाते-रिश्ते के महत्व और उसकी आवश्यकता का प्रत्येक व्यक्ति भली-भाँति अन्दाज़ा कर सकता है। जो व्यक्ति रिश्ते-नाते का आदर न करता हो और सगे-सम्बन्धियों का हक़ न पहचानता हो वह ईश्वर के दूसरे बन्दों के साथ कैसे इन्साफ़ करेगा और वह दूसरों का हमदर्द और उनका दुख बाँटनेवाला कैसे होगा। जो व्यक्ति अपने क़रीबी रिश्तेदारों और निकट सम्बन्धियों के लिए पराया बन जाता हो, वास्तव में तो वह मर चुका होता है। जीवन के सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कुछ कर सकेगा उससे इसकी आशा नहीं की जा सकती।
मानव-प्राण का सम्मान
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मोमिन अपने धर्म की असंकीर्णता में निरन्तर उस समय तक रहता (और लाभ उठाता रहता) है जब तक कि वह किसी हराम (प्रतिष्ठित) ख़ून को नहीं बहाता।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात् जब तक मोमिन नाहक़ क़त्ल का दोषी नहीं होता धर्म में उसके लिए निरन्तर कुशादगी ही कुशादगी होती है। इससे एक बड़ा तथ्य यह मालूम होता है कि धर्म ईमानवालों के लिए तंगी पैदा नहीं करता, बल्कि मोमिन का धर्म तो उसके लिए सर्वथा कुशादगी और आशा और शुभ सूचना होता है। तंगी और ईश्वर की रहमतों से दूरी का कारण तो आदमी के अपने दुष्कर्म होते हैं। ये और इस प्रकार की कितनी ही हदीसें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इनसान की जान को ईश्वर की दृष्टि में बड़ा सम्मान प्राप्त है। नाहक़ क़त्ल एक जघन्य अपराध है। इसे कोई मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन सबसे पहली चीज़ जिसका निर्णय लोगों के बीच किया जाएगा वह ख़ून का दावा है।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
ईश्वर के अधिकारों में सबसे पहले नमाज़ के प्रति पूछा जाएगा और बन्दों के अधिकारों के सिलसिले में सबसे पहले क़त्ल के मुक़द्दमे का निर्णय किया जाएगा। इसलिए कि किसी नाहक़ ख़ून को बहानेवाला वास्तव में मानव-प्राण के आदरणीय होने को स्वीकार ही नहीं करता। हालाँकि लोगों के अधिकारों में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ यह है कि मानव-प्राण का सम्मान किया जाए। फिर उसके बाद उसके दूसरे अधिकार सामने आते हैं जिन के हनन के सम्बन्ध में फ़ैसले नाहक़ क़त्ल के फ़ैसले के बाद ही किए जाएँगे।
प्रेम और करुणा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि मोमिन नहीं बनते, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि परस्पर एक-दूसरे से प्रेम न करो। क्या मैं तुम्हें वह कर्म न बताऊँ जिसको तुम करो तो तुम परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करने लगोगे। वह यह कि आपस में सलाम को रिवाज दो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : स्वर्ग घृणा और कपट-द्वेष की जगह कदापि नहीं है। उसमें तो वे लोग प्रवेश करेंगे जिनके हृदयों का पोषण घृणा और द्वेष ने नहीं, प्रेम ने किया होगा। जिनके पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम और सौहार्द के आधार पर सुदृढ़ होंगे। वे एक-दूसरे से घृणा नहीं प्रेम करनेवाले होंगे और इसे वे ठीक अपने ईमान का तक़ाज़ा समझते होंगे।
इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक आसान और व्यावहारिक उपाय का उल्लेख किया है और वह यह कि मोमिन अपने समाज में एक-दूसरे से बेगाना बनकर न रहें बल्कि जब वे आपस में मिलें तो एक-दूसरे को सलाम करें और उनका यह सलाम मात्र औपचारिकता बनकर न रहे, बल्कि उसके पीछे सही भावना और सम्यक् विचार कार्यरत हो। वे सलाम करके दिल से यह बात ज़ाहिर कर रहे हों कि वे दुनिया और आख़िरत में एक-दूसरे की सलामती और भलाई और कामयाबी की इच्छा रखते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सलाम के इस्लामी तरीक़े को अगर समाज में रिवाज दिया जाए तो लोगों के दिलों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना उभर सकती है।
हदीस का अर्थ यह नहीं है कि सलाम ही वह एकमात्र साधन है जिसे अपनाकर लोगों में प्रेम पैदा हो सकता है, बल्कि उपाय और भी हैं। इस हदीस में एक विशेष उपाय का उल्लेख किया गया है। इस्लाम ने सामाजिकता के जिन नियमों की शिक्षा दी है वे सभी ऐसे हैं जो घृणा को नहीं बल्कि पारस्परिक प्रेम और अनुराग ही को शक्ति देनेवाले हैं।
(2) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह के बन्दों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो यद्यपि न नबी हैं और न शहीद लेकिन क़ियामत के दिन ईश्वर के यहाँ उनके स्थान को देखकर नबी और शहीद उनके सदृश होना चाहेंगे।" सहाबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! हमें बताएँ कि वे कौन लोग हैं? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ये वे लोग हैं जिन्होंने मात्र 'राहे-ख़ुदावन्दी' के कारण परस्पर एक-दूसरे से प्रेम किया हालाँकि उनके बीच न तो कोई वंशीय सम्बन्ध होता है और न आर्थिक लेन-देन का कोई मामला। अतः ईश्वर की सौगन्ध! उनके चेहरे नूर (या सर्वथा नूर) होंगे। और वे नूर पर होंगे। न तो वे डर रहे होंगे जबकि आम लोगों में भय व्याप्त होगा और न वे शोकाकुल होंगे जबकि आम लोग शोकग्रस्त होंगे।” इस मौक़े पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की यह आयत पढ़ी, "अला इन्-न औलियाअल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यह-ज़नून।" (सुन लो अल्लाह के दोस्तों को न तो कोई भय होगा, न वे शोकाकुल होंगे। (10:62) (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से स्पष्ट होता है कि इस प्रेम और अनुराग का कितना अधिक महत्व और मूल्य है जिसके पीछे कोई तुच्छ इच्छा और सांसारिक लोभ कार्यरत न हो बल्कि वह प्रेम विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए हो। हदीस के मूल में शब्द 'बिरौहिल्लाह' प्रयुक्त हुआ है। इसे ‘बिरूहिल्लाह’ भी पढ़ा गया है। दोनों का सार एक ही है जो रूह के सदृश है, अर्थात जीवन का जो मूल है वह ईश्वर की ख़ास रहमत और अनुग्रह ही है। प्रत्येक स्थिति में दोनों का आशय एक ही है कि उनके प्रेम के पीछे कोई भौतिक एवं आर्थिक प्रयोजन नहीं, बल्कि यह मात्र ईश्वरीय सम्बन्ध का आनन्द और उसका माधुर्य है जिसकी अभिव्यक्ति पारस्परिक प्रेम और एकात्मता के रूप में होती है। जिस प्रकार ईश्वर की दया और अनुकम्पा क़ुरआन और मार्गदर्शन के रूप में दुनिया में प्रकट होती है उसी प्रकार यह भी ईश्वरीय मार्गदर्शन और ईश्वरीय अनुकम्पा है जिसके कारण ईमानवाले परस्पर प्रेमभाव रखते हैं।
इस हदीस में यह जो कहा गया है कि नबी और शहीद विशुद्ध रूप से ईश्वर के लिए प्रेम करनेवालों के सदृश होना चाहेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्थान और श्रेणी की दृष्टि से नबियों और शहीदों से श्रेष्ठ होंगे। कभी ऐसा होता है कि कम दर्जे के किसी आदमी की कोई हालत ऊँचे दर्जे के लोगों को भी आकर्षक प्रतीत होती है। इसी को इस हदीस में सदृशता चाहने से अभिव्यंजित किया गया है। अर्थात् सदृशता चाहने से अभिप्राय यहाँ प्रशंसा और क़द्रदानी है।
(3) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे पास आए और कहा—
“क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के निकट कौन-सा अमल अत्यन्त प्रिय है?” किसी ने कहा कि नमाज़ और ज़कात और किसी ने कहा कि जिहाद। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अल्लाह की दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय और पसन्दीदा कर्म है अल्लाह के लिए प्रेम और अल्लाह के लिए द्वेष।” (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात धर्म में मौलिक चीज़ ईश्वर की दृष्टि में वह प्रेम है जो अल्लाह के लिए हो और अगर किसी से द्वेष या वैर हो तो वह भी अल्लाह ही के लिए हो। आदमी की पसन्द और नापसन्द का वास्तविक मानदण्ड यही होना चाहिए। यही समस्त इबादतों और नेक कामों का आधार है। अल्लाह के लिए प्रेम और अल्लाह के लिए द्वेष, वास्तव में यही धर्म की मूल आत्मा है। इसलिए इसे दूसरे समस्त नेक कर्मों के मुक़ाबले में विशिष्टता प्राप्त है।
इसी लिए इमाम इब्ने-तैमिया ने अपने एक फ़तवे में ईशप्रेम को 'मूल धर्म' अर्थात धर्म का मूल और आधार ठहराया है। अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही ने सूरा इख़्लास की व्याख्या में लिखा है—
“जिस प्रकार प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य और एक अन्तिम आशय होता है जिसपर वह कार्य समाप्त हो जाता है उसी प्रकार ईमान और क़ुरआनी शिक्षा का अन्तिम अभिप्राय ईश-प्रेम है। समस्त नबियों की शिक्षा का केन्द्र और सारतत्व यही था। और आध्यात्मिक जीवन इसी का नाम है। क़ुरआन तो इस शिक्षा से परिपूर्ण है। मगर तौरात और इंजील में भी यह आदेश स्पष्टतः सुना दिया गया है। ईसा (अलैहिस्सलाम) से पूछा गया कि तौरात के आदेशों में सर्वोच्च आदेश क्या है? तो कहा, ईश्वर से सम्पूर्ण हृदय, सम्पूर्ण आत्मा, सम्पूर्ण बुद्धि और विवेक से प्रेम करना, यही सर्वप्रथम और महानतम आदेश है।"
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन अल्लाह कहेगा कि कहाँ हैं वे लोग जो मेरी महानता और प्रताप के निमित्त परस्पर प्रेम करते थे? आज मैं उन्हें अपनी छाया में जगह दूँगा जबकि आज मेरी छाया के सिवा कोई छाया नहीं है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : ईश-प्रियता की अपेक्षा यह है कि बन्दा उससे प्रेम रखे और यह प्रेम अपेक्षा रखता है कि ईश्वर के मोमिन बन्दों से प्रेम का सम्बन्ध सुदृढ़ किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा यह रवैया ईश्वरीय महानता और प्रताप को एक चुनौती होगी। और यह एक ऐसा दोष होगा जो हमें अल्लाह की रहमत की छाया से वंचित कर देगा।
(5) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी बन्दे ने ईश्वर के लिए किसी बन्दे से प्रेम किया उस ने वास्तव में अपने महान और प्रतापवान रब की बड़ाई और श्रेष्ठता का आदर किया।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : किसी से जो हार्दिक सम्बन्ध ईश्वर के लिए हो उसके महत्व और मूल्य का अन्दाज़ा करने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन मर्मज्ञों के लिए पर्याप्त है कि अल्लाह के लिए किसी से प्रेम अखिल जगत् के प्रभु की बड़ाई और श्रेष्ठता के आदर के समानार्थक है।
(6) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि—
"अल्लाह कहता है कि उन लोगों से प्रेम करना मुझपर अनिवार्य है जो मेरे लिए परस्पर प्रेम करते हैं, मेरे लिए एक साथ बैठते हैं और मेरे लिए एक-दूसरे से मिलते हैं और मेरे लिए एक-दूसरे पर माल ख़र्च करते हैं।" (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : इसके पीछे भी प्रेम ही काम करता है कि वे एक-दूसरे के पास बैठते, एक-दूसरे से मिलते और एक-दूसरे पर अपना धन ख़र्च करने में झिझकते नहीं। लेकिन उनका यह सब कुछ अपने ईश्वर के लिए होता है। वे उसकी प्रसन्नता के अभिलाषी और इच्छुक होते हैं। उसी के लिए वे जीते हैं और उसी के लिए वे मरना भी चाहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उनके जीवन की मूल निधि और उसके सामीप्य की अभिलाषा उनके जीवन की उपलब्धि होती है। उनकी उच्चता और उनके मक़ाम का अन्दाज़ा भौतिकवादी निगाहें कदापि नहीं कर सकतीं।
(7) हज़रत बराअ् बिन-आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हुदैबिया के दिन तीन बातों पर सन्धि की थी। एक यह कि बहुदेववादियों में से जो व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आए तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसे वापस कर देंगे। दूसरे यह कि मुसलमानों में से जो व्यक्ति बहुदेववादियों के पास चला जाए वे उसे वापस नहीं करेंगे। तीसरे यह कि अगले साल आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का में प्रवेश करें और (उमरा अर्थात् काबा के दर्शन के लिए) केवल तीन दिन वहाँ ठहरें। अतएव जब (अगले साल) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का आए और नियत अवधि पूरी हो गई और आप मक्का से निकलने लगे तो हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेटी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पीछे यह कहती हुई दौड़ी कि ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे चचा! हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसे अपने साथ ले जाने का इरादा किया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसके लिए हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बीच विवाद हुआ। हजरत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि मैंने इसे अपने साथ लिया है और यह मेरे चचा की बेटी है और इसकी मौसी (ख़ाला) मेरे निकाह में है। हज़रत ज़ैद कह रहे थे कि यह मेरी भतीजी होती है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस विवाद का निर्णय इस प्रकार किया कि उस लड़की को उसकी ख़ाला के हवाले कर दिया जाए और कहा, "ख़ाला माँ के समान है।" और आपने हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा, "तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ।" हज़रत जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा, “शारीरिक और नैतिक दृष्टि से तुम मेरे सदृश हो।” और आपने हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा, “तुम मेरे भाई और प्रिय हो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा थे लेकिन वे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दूध-शरीक भाई भी होते थे। अबू-लहब की लौंडी सूबिया का दूध आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने और हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने भी पिया था। इसी लिए हज़रत हमज़ा की बेटी ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को 'ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे चचा!' कहकर पुकारा था। स्पष्ट रहे कि हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) उहुद के युद्ध (3 हिजरी) में शहीद हो गए थे और इस हदीस में हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेटी से सम्बन्धित जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह हुदैबिया की सन्धि (6 हिजरी) के दूसरे साल की घटना है।
हज़रत जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के भाई थे और वे हज़रत अली से उम्र में दस साल बड़े थे।
हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा आज़ाद किए गए ग़ुलाम और गोद ली हुई सन्तान थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) में भाईचारा कराया था इसी लिए हज़रत ज़ैद ने हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेटी को अपनी भतीजी कहा।
ख़ाला ही वास्तव में माँ के पश्चात उसके स्थान पर हो सकती है। इसलिए माँ के बाद ख़ाला ही का घर हो सकता है जहाँ बच्चे को किसी पराएपन का एहसास न हो और हो भी तो बहुत कम।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा कि तुम मेरे सदृश हो और हज़रत ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा कि तुम मेरे भाई और प्रिय हो। यह इच्छा प्रत्येक को थी कि हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेटी का लालन-पालन उसके यहाँ हो। परवरिश के लिए तो आपने उसे उसकी मौसी के हवाले करने का आदेश दिया। लेकिन अपने साथियों का दुखी होना भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सहन न था। उनका रंज दूर हो इसके लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन लोगों के सम्बन्ध में ये बातें कही थीं। इन बातों से उन तीनों की श्रेष्ठता भली-भाँति प्रकट होती है। और यह भी कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनसे कितना अधिक प्रेम था और यह प्रेम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए था।
(8) हज़रत अबू-अय्यूब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि—
“जो व्यक्ति माँ और उसके बेटे के बीच जुदाई डाले तो अल्लाह क़ियामत के दिन उसके और उसके प्रियजनों के बीच जुदाई डाल देगा।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : जुदाई डालने के कई तरीक़े हो सकते हैं। उदाहरणार्थ लौंडी को तो बेच दिया मगर उसके बच्चे को रोक लिया या बच्चे को बेच दिया और उसकी माँ को रहने दिया, या किसी एक को किसी के हाथ और दूसरे को किसी दूसरे के हाथ बेचा।
बेटे और माँ के बीच जुदाई डालने का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया गया है वरन् यही आदेश प्रत्येक छोटे बच्चे और उसके निकटवर्ती नातेदार से जुदा करने का है। चाहे वह माँ हो या बाप या दादा-दादी हों या भाई-बहन। इसी लिए कुछ विद्वानों ने दो भाइयों के बीच, अगर उनमें से एक अभी छोटा है, जुदाई डालने को अवैध ठहराया है।
भावनाओं का आदर
(1) हज़रत मालिक-बिन-हवैरिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम कुछ हमउम्र नवजवान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास (दीन सीखने) आए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास हम लोग बीस दिन रहे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अत्यन्त दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने महसूस किया कि हम घर जाना चाहते हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमसे पूछा कि "तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं?" हमने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बताया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अपने बच्चों में वापस जाओ और उनके बीच रहो और उन्हें (जो कुछ सीखा है) सिखाओ और अमुक नमाज़ अमुक समय पढ़ो और अमुक नमाज़ अमुक समय पढ़ो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : एक हदीस में आया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है और जब नमाज़ का समय आ जाए तो कोई तुममें से अज़ान दे और जो तुममें (ज्ञान और आचरण की दृष्टि से) बड़ा हो वह इमामत करे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
इस हदीस से स्पष्ट है कि दूसरे लोगों की आवश्यकताओं और उनकी भावनाओं आदि का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। धर्म यह नहीं है कि लोगों से उनकी प्राकृतिक भावनाएँ छीन ली जाएँ और उन्हें उनके घरवालों और बीवी-बच्चों से बेपरवाह और विरक्त बना दिया जाए, बल्कि बीवी-बच्चों के बीच रहते हुए ईश्वर की बन्दगी करनी चाहिए और प्रयास इस बात का होना चाहिए कि सगे-सम्बन्धी भी उसी रास्ते को अपना लें जो उसने अपने लिए पसन्द किया है।
अच्छा गुमान
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छा गुमान सर्वोत्तम इबादतों में से है।” (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद)
व्याख्या : अल्लाह का अपने बन्दों पर एक मौलिक अधिकार यह है कि वे अपने रब से बदगुमान न हों बल्कि उनका सम्बन्ध ईश्वर से अच्छा गुमान और अच्छी आशा रखने का हो यहाँ यह बात सामने रहे कि अच्छा गुमान यह नहीं है कि आदमी निरन्तर ईश्वर की अवज्ञा करता रहे और उससे मुक्ति और क्षमादान की आशा रखे। बल्कि ईश्वर से अच्छा गुमान यह है कि आदमी बन्दगी और आज्ञापलन में कोताही से बचे। और इसके पीछे यह भावना कार्यरत हो कि ईश्वर हमारी इबादतों और नेक कामों को नष्ट नहीं होने देगा। वह अपने बन्दों की इबादतों को स्वीकार करता है और उनके नेक कामों का अवमूल्यन नहीं करता।
ईश्वर के बाद हमपर उसके बन्दों का भी यह हक़ और अधिकार होता है कि हमारा मामला उनसे बदगुमानी की बुनियाद पर हरगिज़ न होना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम अकारण किसी से बदगुमान न हों। दुराशा से अपने आप को हमेशा मुक्त रखें। यह इसलिए भी आवश्यक है कि इसके बिना समाज का वातावरण सदैव प्रदूषित रहेगा। और यह इसलिए भी आवश्यक है कि इसके बिना आदमी के चरित्र और उसके व्यक्तित्व में एक दोष पाया जाएगा जो अत्यन्त निकृष्ट होगा।
आदमी में अगर यह ऐब नहीं है कि वह लोगों से निराश हो बल्कि अपने भाइयों के साथ वह अच्छे गुमान रखता है तो यह एक ऐसा गुण होगा जिसके कारण उसके चरित्र और व्यक्तित्व ही में नहीं बल्कि उसके समस्त कर्मों ओर उसकी हर इबादत में सुन्दरता आ जाएगी।
यहाँ यह बात भी दृष्टि में रहे कि अच्छा आदमी दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखता है। बुरे व्यक्ति को ही दूसरों में बुराई की तलाश रहती है।
दूसरों के ऐब छिपाना
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वह उसपर अत्याचार करे और न उसे तबाही के हवाले करे। जो व्यक्ति अपने भाई की आवश्यकतापूर्ति के काम में लगा रहेगा, अल्लाह उसकी आवश्यकतापूर्ति के काम में लगा रहेगा। और जो व्यक्ति किसी मुसलमान पर से कोई विपत्ति दूर करेगा, अल्लाह क़ियामत की मुसीबतों में से कोई मुसीबत उसपर से दूर करेगा। और जो कोई मुसलमान के अवगुणों पर परदा डालेगा, अल्लाह क़ियामत के दिन उसके अवगुणों पर परदा डालेगा।" (हदीस : मुस्लिम)
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो कोई दुनिया में किसी बन्दे के अवगुण पर परदा डालेगा, ईश्वर क़ियामत के दिन उसके अवगुण पर परदा डालेगा।” (हदीस : मुस्लिम)
(3) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“जो मुसलमान अपने भाई की आबरू की प्रतिरक्षा करता है तो अल्लाह पर यह हक़ हो जाता है कि क़ियामत के दिन वह नरक की आग से उसकी सुरक्षा करे।" इसके बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की यह आयत पढ़ी, "और ईमानवालों की सहायता करना तो हमपर एक हक़ है। (30:47) (हदीस : शरहुस-सुन्नह)
व्याख्या : भाई अपने भाई पर लगाए गए आरोपों को दूर करने का पूरा प्रयास करता है ताकि भाई की आबरू की रक्षा हो सके। यह कर्म अल्लाह को इतना पसन्द है कि वह इसके प्रतिफल के रूप में उसे नरक की अग्नि से मुक्ति देगा।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की यह आयत अपनी बात के समर्थन और पुष्टि में प्रस्तुत की। यह आयत बताती है कि ईश्वर अपने मोमिन बन्दों का सहायक और मददगार है। वह उन लोगों को सर्वोत्तम प्रतिफल प्रदान करेगा जो उसके मोमिन बन्दों के सहायक होते हैं। सोचने की बात है कि ईश्वर तो मोमिनों का सहायक और समर्थक हो और हम ईमानवालों की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने और उनके ऐबों को उघाड़ने के लिए प्रयत्नशील हों। आज हम इस बहुमूल्य शिक्षा को भूल बैठे हैं और अपने पतन के स्वयं ज़िम्मेदार हैं।
दूसरों के अवगुणों को छिपाने के सम्बन्ध में जो हदीसें यहाँ प्रस्तुत की गई हैं वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस्लाम इसे जायज़ नहीं समझता कि किसी के ऐबों को खोला जाए। उसका आदेश तो खोलने का नहीं बल्कि उन पर परदा डालने का है। उसे इससे हरगिज़ दिलचस्पी नहीं है कि लोगों से उनकी इज़्ज़त और आबरू छीन ली जाए। इसके विपरीत उसके अन्दर तो अप्रतिष्ठित और पतित लोगों को भी आदर और आबरू प्रदान करने का रुझान पाया जाता है। इस्लाम यूँ तो किसी की मानहानि को पसन्द नहीं करता लेकिन ईमानवालों के मामले में तो वह मुसलमानों को अत्यन्त सचेत करता है कि वे अपने भाई मुसलमानों के अवगुणों को छिपाएँ और यथासम्भव उन्हें मानहानि से बचाएँ। मुसलमानों का यह दायित्व है कि वे अपने मुसलमान भाई की आबरू और उसकी प्रतिष्ठा के संरक्षक बनें चाहे वह भाई अपने निकट रहता हो या दूर, उन्हें प्रत्येक स्थिति में अपने भाई के प्रति शुभकामना से ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए।
राज़दारी
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे सहाबियों में से कोई व्यक्ति किसी की कोई बुराई मुझसे बयान न करे। इसलिए कि मैं इस बात को पसन्द करता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल साफ़ हो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात अगर किसी को किसी व्यक्ति की कोई बुराई या अवगुण मालूम हो तो वह उसका वर्णन मुझसे न करे, उसे राज़ ही रहने दे। मैं चाहता हूँ कि लोगों की ओर से मेरा दिल बिलकुल साफ़ हो। किसी के लिए कोई मलिनता और अप्रसन्नता मेरे दिल में न पैदा हो। लोगों के बारे में मेरा गुमान और विचार अच्छा ही रहे। इसलिए कि अगर किसी पर किसी व्यक्ति की कोई बुराई या अवगुण प्रकट हो जाए तो उसे अपनी ही हद तक रखे। उस रहस्य को प्रकट न करे।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब यह पसन्द था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दिल अपने साथियों के प्रति साफ़ रहे तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम रखनेवाले मुसलमानों की भी यही अभिरुचि होनी चाहिए। उन्हें भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका दिल अपने भाइयों की ओर से साफ़ रहे। कोई घृणा और मलिनता उनके अन्दर न रहे। यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि हम न तो लोगों के अवगुणों की खोज में रहें और न उनके अवगुणों को इधर-उधर बाँटते फिरें। अवगुणों और कमज़ोरियों की जगह हमें लोगों के सद्गुणों और विशेषताओं में दिलचस्पी हो।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिससे परामर्श लिया जाए उसे अमानत सौंपी गई।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात जिस व्यक्ति पर भरोसा करके उससे किसी मामले में परामर्श लिया जाए उसका यह दायित्व होता है कि वह उस भरोसे को कदापि आघात न पहुँचाए। एक तो उसका दायित्व है कि परामर्श सही दे। कोई ग़लत परामर्श अपने भाई को कदापि न दे। दूसरे उसका यह भी दायित्व है कि जिस मामले में उससे परामर्श लिया जाए वह उसे एक अमानत समझते हुए पूर्ण गोपनीयता से काम ले और भाई का राज़ हरगिज़ प्रकट न करे। इसलिए कि बहुत सम्भव है कि परामर्श लेनेवाला व्यक्ति इस बात को पसन्द न करता हो कि कोई व्यक्ति उससे अवगत हो। और अगर उसने यह कह भी दिया हो कि इसे कोई दूसरा व्यक्ति न जाने तो इस स्थिति में तो यह दायित्व और भी बढ़ जाता है कि उसका रहस्य प्रकट न हो।
(3) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपनी-अपनी आवश्यकतापूर्ति में सफल होने के लिए गोपनीयता से मदद लो, क्योंकि प्रत्येक साधन-सम्पन्न से ईर्ष्या की जाती है।" (हदीस : अल-मोअजम लित्तबरानी)
व्याख्या : दुनिया में ईर्ष्यालुओं की कमी नहीं होती। वे जिस व्यक्ति को सफल होते देखते हैं उससे इर्ष्या करने लग जाते हैं। किसी की पदोन्नति उन्हें गवारा नहीं होती। वे कभी पसन्द नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अपनी योजनाओं और इरादों में सफल हो। इसलिए आवश्यक है कि आदमी अपनी योजनाओं और इरादों को समयपूर्व लोगों पर हरगिज़ प्रकट न करे। बहुत सम्भव है ऐसी स्थिति में उससे इर्ष्या करनेवाले उसके लिए कठिनाइयाँ और बाधाएँ खड़ी कर दें। यूँ भी आदमी को हलके पेट का नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक अपनी योजनाओं का लोगों में प्रचार करता फिरे और इर्ष्यालुओं को इसका अवसर प्रदान कर दे कि वे उसे अपनी ईर्ष्या का निशाना बनाएँ।
लोगों की आवश्यकतापूर्ति
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि—
“जो व्यक्ति मेरी उम्मत में से किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करे और इससे उसका उद्देश्य उसे प्रसन्न करना हो तो उसने मुझे प्रसन्न किया और जिस व्यक्ति ने मुझे प्रसन्न किया उस ने अल्लाह को प्रसन्न किया और जिस किसी ने अल्लाह को प्रसन्न किया उसे अल्लाह स्वर्ग में प्रवेश कराएगा।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपनी उम्मत (समुदाय) के व्यक्तियों से जो विशेष लगाव था वह इस हदीस से स्पष्टतः प्रकट है। फिर इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि किसी की आवश्यकता पूरी करना और उसके लिए ख़ुशी का सामान करना दीन में क्या दर्जा रखता है। यह हदीस बताती है कि दूसरों को ख़ुश देखने की इच्छा अत्यन्त प्रिय इच्छा है। यह इच्छा आदमी के अन्दर उसी स्थिति में उभर सकती है जबकि उसे ईश्वर के बन्दों से गहरा और भावनात्मक लगाव हो और वह उनके कष्ट और परेशानी को देखकर विकल हो जाता हो।
किसी ज़रूरतमन्द की ज़रूरत पूरी करने का प्रेरक न स्वार्थपरता हो और न सांसारिकता। ज़रूरतमन्द को प्रसन्न और सुखी देखने की इच्छा स्वयं एक सशक्त प्रेरक है, और कदाचित सबसे सशक्त। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि आदमी के पास सहानुभूति और दूसरे के ग़म दूर करने की भावना मौजूद हो। यही सहानुभूति, संवेदनशीलता और ग़म दूर करने की भावना है जिसके कारण कोई व्यक्ति मानवता के सर्वोच्च स्थान पर आसीन होता है और जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होता है। यह भाव अगर विलुप्त हो जाए तो मानव की मानवता की दृष्टि से मृत्यु हो जाती है यद्यपि देखने में वह धरती पर चलता-फिरता, लोगों से बातें करता और अपनी उपस्थिति का ऐलान करता हो। किसी व्यक्ति के जीवन का प्रमाण न तो उसकी ऊँची और गगनचुंबी इमारतों से होता है और न किताबों, अख़बारी वक्तव्यों और आलेखों के द्वारा मिलता है और न लाउडस्पीकर और रेडियो उसके जीवन का प्रमाण देते हैं। किसी के जीवन का प्रमाण तो उसकी उन सेवाओं से मिलता है जो मानवजाति के लिए वह कर रहा होता है। किसी व्यक्ति के विषय में यह जानने का कि उसे जीवन प्राप्त है भरोसेमन्द साधन यही है। इससे प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि वह कितना जीवित है।
यह हदीस बताती है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हृदय में लोगों के प्रति कितनी करुणा है। लोगों का दुख आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दुखी कर देता है और लोगों की प्रसन्नता से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी लिए कहा कि जिसने किसी ज़रूरतमन्द व्यक्ति की आवश्यकता पूरी की और उसके पीछे दिखावा आदि कोई तुच्छ कोटि की इच्छा न थी बल्कि ज़रूरतमन्द और परेशान व्यक्ति को प्रसन्न देखना उसका उद्देश्य था, उसने मुझे ख़ुश किया। और मुझे ही नहीं उसने अपने इस कर्म के द्वारा अपने ईश्वर को प्रसन्न किया, और जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो उसके सौभाग्य का क्या कहना! यह सम्भव नहीं कि ईश्वर उससे प्रसन्न हो और उसे अपनी नेमतें न प्रदान करे। इसकी आशा तो एक साधारण व्यक्ति से भी नहीं की जाती। इसलिए अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को ईश्वर स्वर्ग में जगह प्रदान करेगा। इस हदीस में हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शन है। दूसरों के लिए प्रसन्नता का साधन उपलब्ध कराना महानतम कार्यों में से है। अगर यह विचार अपने सही अर्थों में हमारे अन्दर पैदा हो जाए तो क्या हम किसी को दुख दे सकते हैं? क्या हम कभी यह पसन्द कर सकते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई कष्ट पहुँचे? हम तो उस अत्याचार से भी बेचैन हो उठेंगे जो दूसरों ने किसी पर किया हो।
किसी आवश्यकतापूर्ति का महत्व और मूल्य उस स्थिति में और भी बढ़ जाता है जब कोई किसी मोमिन की आवश्यकता पूरी करता है। इसलिए कि मोमिन व्यक्ति ईश्वर का अत्यन्त निकटवर्ती होता है।
किसी की आवश्यकतापूर्ति और उसकी फ़रियाद सुनना अल्लाह को कितना पसन्द है इसका अन्दाज़ा इस हदीस से भी किया जा सकता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने दुखी, अत्याचारग्रसित और विकल की फ़रियाद सुनी, ईश्वर उसके लिए तिहत्तर क्षमादान अनिवार्य कर देता है। उनमें से केवल एक ही से उसके काम और मामलों की दुरुस्ती हो जाती है। शेष बहत्तर क्षमादान क़ियामत के दिन उसकी पदोन्नति का कारण होंगे।" (हदीस : बैहक़ी)
'ग़-फ़-र' का अर्थ है ढाँकना, क्षमा करना और ठीक करना। क़ुरआन में कुछ ऐसे अवसरों पर भी क्षमा का उल्लेख किया गया है। जहाँ किसी गुनाह और अवज्ञा की बात वर्णित नहीं हुई है। इससे ज्ञात होता है कि क्षमादान के अर्थ में व्यापकता पाई जाती है। ईश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे यह भी क्षमादान है और वह हमारे अवगुणों को छिपा ले और हमें अपमान से बचा ले, क्षमादान का यह भी एक रूप है। इस हदीस से ज्ञात हुआ कि मोमिन के दर्जों का बुलन्द किया जाना भी क्षमादान का एक रूप है। क़ुरआन में है—
“उनकी बात दूसरी है जिन्होंने धैर्य से काम लिया और सत्कर्म किए। वही हैं जिनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान है।" (11:11)
इस्लाम में प्रत्येक अभीष्ट कर्म वास्तव में उस स्थान की ओर संकेत करता है जो सर्वाधिक उच्च है और जिस स्थान पर पहुँचा हुआ व्यक्ति किसी भलाई और प्रतिफल से वंचित नहीं हो सकता। एक साधारण नेकी भी अगर कोई पूरी चेतना और समझ के साथ करे तो एक ओर तो उसके प्रभावस्वरूप वह दूसरी समस्त नेकियों को भी स्वभावतः अपना सकेगा और दूसरी ओर बुराइयों से भी उसे अत्यन्त घृणा हो जाएगी। एक छोटी नेकी के अन्दर भी सम्पूर्ण जीवन को बदल देने की शक्ति निहित है। एक नेकी भी अगर सही अर्थों में नेकी है तो वह इसका लक्षण होती है कि आदमी सन्मार्ग पर है। इसी लिए हम अल्लाह के रसूल को किसी एक नेकी पर स्वर्ग की शुभ सूचना देते हुए पाते हैं। इससे किसी को यह भ्रम न होना चाहिए कि किसी का जीवन अत्याचारों, क्रूरताओं और अवज्ञाओं से भरा हुआ है वह मात्र एक नेकी के बलबूते पर स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। ऐसे व्यक्ति की तो वह नेकी वस्तुतः नेकी नहीं होती। उस नेकी को तो उसका अपना जीवन ही रद कर देता है। वास्तविक नेकी वह है जो आदमी के सम्पूर्ण जीवन के होने की सूचना दे सके।
जिस प्रकार दृष्टिवान के लिए सूर्य का ढलना, उसका अस्त होना और अरुणोदय यह सब इसकी अपेक्षा करते हैं कि वह इन घड़ियों में ईश्वर के आगे सज्दा करे। अब अगर कोई इन घड़ियों में ईश्वर के आगे अपने को नहीं झुकाता और उसके सामने विनम्रता और दीनता प्रकट नहीं करता, वह सृष्टि-सत्यों को झुठलाता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति देखता है कि किसी याचक की कातर दृष्टि किसी दुख बाँटनेवाले की तलाश में इधर-उधर भटक रही है और वह उसकी ख़बर नहीं लेता तो वह एक ओर तो उस भावना को कुचलकर रख देता है जो जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान रत्न है, जिसको ईश्वर ने उसके हृदय में अमानत के तौर पर रखा है और दूसरी ओर वह उस तक़ाज़े को भी निरर्थक समझता है जो उसके समक्ष याचक के कातर नेत्रों के रूप में सामने आया है। किसी की यह विवशता और कातरता एक दर्पण बन कर उसके सम्मुख आई लेकिन उस दर्पण में उसका अपना बिम्ब जो उभरा वह कैसा है? इसको आप स्वयं समझ सकते हैं। भौतिक दर्पण केवल हमारे बाह्य रूप को प्रकट करते हैं लेकिन ये दर्पण जो विवशताओं, मजबूरियों और उत्पीड़नों के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनके द्वारा हमारे अन्दरून की तस्वीर उभरती है जो बता देती है कि हमारी मनोदशा कैसी है।
आप कितने ही ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके यहाँ धन-सम्पत्ति की कोई कमी नहीं लेकिन हृदय उनके कठोर हैं। वे किसी के काम आने के नहीं, और कितने ही तंगदस्त हैं लेकिन सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना उनमें पाई जाती है। दूसरों के लिए जो कुछ बन पड़ता है करते हैं। कुछ नहीं तो किसी का कष्ट और विपत्ति देखकर इस प्रकार रो पड़ते हैं मानो वह विपत्ति स्वयं उनपर आ पड़ी है। किसी कवि ने कहा है—
हाथ रिक्त हैं यद्यपि अपने
किन्तु अनुग्रह मुझपर यह है
दिया हृदय वह मेरे प्रभु ने
दया, आर्द्रता से परिचित जो!
सहानुभूति और संवेदनशीलता का अभाव एक ऐसा अभाव है जिसके कारण लोग कभी भी उच्च नहीं हो सकते। चाहे वे हमें देखने में कितने ही बड़े पद पर आसीन दिखाई देते हों। चाहे उनके पास धन-सम्पत्ति की कितनी ही रेल-पेल क्यों न हो। उनके चरित्र में पाई जाने वाली कमी को इनमें से कोई वस्तु दूर नहीं कर सकती।
हमदर्दी और दुख बाँटने की भावना अगर है तो इसका प्रभाव आदमी के अपने घरेलू जीवन में भी दृष्टिगोचर होगा। वह अपने घरवालों के साथ मेहरबान होगा। उसका हाल उस बाप जैसा न होगा जिसका बेटा उसकी क्रूरता से परेशान और भयभीत रहता हो।
बड़ों की पहचान यह है कि वे मन-मस्तिष्क ही के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी आहार संचित करते हैं। वे कितने ही अनाथों और असहायों से प्रेम करते हैं। ईश्वर जिनको सुख और वैभव प्रदान करता है वे बड़ी परीक्षा में होते हैं। साधारणतः लोग इस परीक्षा में असफल सिद्ध होते हैं। ऐसे लोग न्याय करना भूल जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि अत्याचार की नीति अपनाकर वे सर्वप्रथम स्वयं पर अत्याचार करते हैं।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कमज़ोर, विधवा महिला और मुहताज और निर्धन व्यक्ति की सहायता के लिए दौड़-धूप करनेवाला उस व्यक्ति की तरह है जो ईश्वरीय मार्ग में सक्रियता दिखाता है।" उल्लेखर्ता कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह भी कहा, “ऐसा व्यक्ति रात्रि में खड़े होनेवाले (इबादत करनेवाले) की तरह है जो इबादत से थकता नहीं या उस रोज़ेदार की तरह है जो निरन्तर रोज़े रखता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करनेवाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करनेवाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहनेवाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखनेवाले की तरह है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, शेख़ैन, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने-माजा)
यह हदीस बताती है कि ज़रूरतमन्दों की देख-भाल हो या ईश्वरीय मार्ग में जिहाद और नमाज़ और रोज़ा, इन सबकी आत्मा एक ही है। ये समस्त कर्म एक ऐसी नैतिकता और चरित्र के परिचायक हैं जो इस्लाम में मूलतः अपेक्षित है। यह नैतिक उच्चता ही है कि बन्दा ईश्वर के आगे विनम्रता और भक्तिभाव और उससे अपने मधुर सम्बन्ध का प्रदर्शन रात में जागकर और दिन में रोज़ों के द्वारा करे। और यह भी मोमिन का चरित्र है कि वह धरती से उपद्रव और बिगाड़ को दूर करने और ईश्वरीय धर्म की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। और फिर यह भी इस्लामी नैतिकता है कि आदमी उन लोगों की मदद से अपना हाथ न खींचे जो सहायता के योग्य हों, चाहे वह कोई विधवा स्त्री हो या कोई वंचित और अभावग्रस्त व्यक्ति।
यह हदीस इस भ्रम को (जो अकसर धार्मिक लोगों में पाया जाता है) दूर करने के लिए पर्याप्त है कि दीन में नमाज़ और रोज़ा आदि इबादतें ही सब कुछ हैं, वे सत्कर्म जिन का सम्बन्ध ईश्वर के बन्दों की सेवाओं से है उनका कुछ अधिक महत्व नहीं है।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने भाई की सहायता करो चाहे वह अत्याचारी हो या उस पर अत्याचार हुआ हो।" एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, "जिस पर अत्याचार हुआ हो उसकी सहायता तो मैं करता हूँ मगर अत्याचारी की सहायता कैसे करूँ?" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुम उसे अत्याचार से रोक दो, यही तुम्हारी ओर से उसकी सहायता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इसमें क्या सन्देह हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अत्याचारी होने की जघन्यता से उसे मुक्त करना उसकी सबसे बड़ी सहायता है, चाहे वह अत्याचारी व्यक्ति उस समय इसे न समझ सके।
सिफ़ारिश
(1) हज़रत समुरह-बिन-जुन्दुब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बेहतरीन सद्क़ा वह सिफ़ारिश है जिसके द्वारा किसी गर्दन को छुड़ाया जाए।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : किसी मुहताज और अभावग्रस्त व्यक्ति को सद्क़ा देकर हम उसे आर्थिक परेशानी से निकालने का प्रयास करते हैं। आर्थिक परेशानी से बढ़कर मुसीबत की बात यह है कि कोई व्यक्ति दासता का जीवन व्यतीत कर रहा हो, किसी की गर्दन फँसी हुई हो या कोई अत्याचारों के बोझ तले कराह रहा हो। इसलिए उसे इस मुसीबत से मुक्ति दिलाने का प्रयास और सिफ़ारिश आम सदक़ों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस सिफ़ारिश को सर्वोत्तम सदक़ा क़रार दिया है।
(2) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मोमिन मोमिन के लिए भवन के सदृश होता है जिसके एक भाग को दूसरे भाग से बल मिलता है।" फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी अँगुलियों को परस्पर मिलाकर दिखाया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बैठे ही थे कि एक व्यक्ति कुछ माँगने को या कोई ज़रूरत लेकर आया।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हम लोगों की ओर उन्मुख हुए और कहा, “सिफ़ारिश करो, तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। और अल्लाह अपने नबी के मुख से जो चाहता है आदेश जारी करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास जब कोई व्यक्ति कोई ज़रूरत लेकर आता तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने साथियों से कहते कि सिफ़ारिश करो कि तुम्हें प्रतिदान मिलेगा और अल्लाह अपने नबी के मुख से जो चाहता है आदेश जारी करता है। अर्थात तुम सिफ़ारिश करके प्रतिदान प्राप्त करो, मैं वही निर्णय करूँगा जो हक़ होगा। नव्वी ने कहा है कि सिफ़ारिश शासक और प्रत्येक व्यक्ति से की जा सकती है चाहे यह सिफ़ारिश किसी को कुछ दिलाने के लिए हो या अत्याचार को रोकने या दण्ड की क्षमा के लिए हो। अलबत्ता किताब और सुन्नत द्वारा निर्धारित दण्ड के मामले में सिफ़ारिश नहीं की जा सकती।
सादगी
(1) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्हें यमन भेजने लगे तो कहा—
"देखना, विलासी जीवन से दूर रहना, क्योंकि अल्लाह के बन्दे विलासी जीवन व्यतीत नहीं करते।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : इस हदीस में भोग-विलास से बचने की शिक्षा दी गई है। मूल अरबी में शब्द 'तनअ्उम' आया है। उससे अभिप्राय वह जीवन है जो मर्यादाहीन और विलासिता का हो। संसार और सांसारिक भोग-विलास की इच्छा मूलतः वे लोग करते हैं जो न ईश्वर पर ईमान रखते हैं और न आख़िरत का विश्वास उन्हें प्राप्त होता है। अधर्मियों के समक्ष संसार और केवल सांसारिक जीवन ही होता है। अतएव क़ुरआन में है—
“छोड़ो उन्हें, खाएँ और मज़े उड़ाएँ और (लम्बी) आशा उन्हें भुलावे में डाले रखे। उन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा।” (15:3)
एक दूसरी जगह है—
“और वे लोग जिन्होंने इनकार किया, वे कुछ ही दिनों का सुख भोग रहे हैं और खा रहे हैं, जिस तरह चौपाए खाते हैं। और आग उनका ठिकाना है।" (47:12)
एक जगह कहा गया है—
“निस्सन्देह वे (विधर्मी) इससे पहले सुख-सम्पन्न थे।” (56:45)
जिन लोगों के सामने आख़िरत का जीवन न होगा, जिनके समक्ष संसार और केवल संसार होगा, उनका सारा ध्यान सांसारिक भोग-विलास की ओर होगा। इसलिए उनकी सारी ऊर्जा इसी सांसारिक साज-सज्जा की प्राप्ति में व्यय होगी। इससे आगे वे कुछ सोच ही नहीं सकते। भौतिकवादी जीवन से उच्च भी कोई जीवन हो सकता है इससे वे सर्वथा अनभिज्ञ होंगे जबकि इस नश्वर सुखोपभोग पर प्रसन्न होने और सन्तुष्ट हो जाने की अपेक्षा आख़िरत के श्रेष्ठतर और स्थायी जीवन की इच्छा और प्रतीक्षा में भौतिकवादी जीवन से कहीं अधिक जीवन का अर्थ पाया जाता है।
यहाँ यह दृष्टि में रहे कि 'तनअ्उम' और 'तजम्मुल' में बड़ा अन्तर है। इस्लाम में तजम्मुल अर्थात सफ़ाई-सुथराई, पवित्रता और परिधानों में सुरुचि का ध्यान रखना पसन्दीदा है। लेकिन इसमें अगर हद से आगे बढ़ते हैं तो तनअ्उम की सीमा प्रारम्भ हो जाती है जिसका फिर कोई अन्त नहीं है। और अगर तजम्मुल में हद से पीछे हटते हैं तो फिर इससे संन्यास का द्वार खुलता है। इन दोनों प्रकार के अतिवाद से बचते हुए मध्यमार्ग अपनाने की शिक्षा ही वास्तव में इस्लाम ने अपने अनुयायियों को दी है।
मासूमियत
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन भोला-भाला, सज्जन और उदार होता है। और दुराचारी सयाना, कृपण और अभागा होता है।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मतलब यह है कि मोमिन कम-समझ और नादान नहीं होता लेकिन अपनी उदार प्रकृति और नैतिक सौन्दर्य के कारण दूसरों के साथ उसका मामला सुविधाजनक और नर्मी पर आधारित होता है। वह धोखा खा जाए यह तो सम्भव है लेकिन उससे इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी व्यक्ति को धोखा देगा। इसके विपरीत दुराचारी व्यक्ति अत्यन्त धूर्त और सयाना होता है। उसमें नैतिक उच्चता नहीं पाई जा सकती। वह धोखेबाज़ होता है। उससे हमेशा कृपणता और हानि की आशंका बनी रहती है।
यहाँ यह दृष्टि में रहे कि मोमिन को कोई व्यक्ति बार-बार धोखा नहीं दे सकता। वह अनुभवों को कभी नज़रअन्दाज़ नहीं करता। अनुभवों से लाभ उठाता है। अतएव एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन एक सूराख़ से दो बार नहीं डसा जाता।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद)
(3)
गरिमा और महानता
शालीनता और गरिमा
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अरफ़ा के दिन हम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ जा रहे थे। इतने में सख़्त डाँटने, मारने और ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज़ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सुनी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने कोड़े से उनकी ओर संकेत करके कहा “ऐ लोगो! शान्ति धारण करो क्योंकि तेज़ी और जल्दबाज़ी सत्कर्म और आज्ञापालन नहीं है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात अनावश्यक भाग-दौड़ करने और जल्दबाज़ी दिखाने को नेकी और आज्ञापलन नहीं कहते, बल्कि जो चीज़ अपेक्षित है वह सुकून और शान्ति है। हमेशा गरिमा और शालीनता का ख़याल रखना ही मोमिन के मर्यादानुकूल है। क़ुरआन में भी है—
“रहमान के बन्दे वे हैं जो धरती पर विनम्रतापूर्वक चलते हैं।" (25:63)
नर्मी और सहनशीलता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक देहाती व्यक्ति ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। लोग उसपर बिगड़ने लगे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहा दो। तुम तो आसानी पैदा करने ही के लिए भेजे गए हो। तुम सख़्ती और दुश्वारी पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात तुम्हें कठोर बनाकर दुनिया में नहीं भेजा गया है। तुम जिस सन्देश को लेकर उठे हो, वह सर्वथा रहमत है। वह इसलिए आया है कि इनसानों की कठिनाइयाँ और बाधाएँ दूर हों, और वे बन्धन तोड़ दिए जाएँ जिनमें वे जकड़े हुए हैं। तुमको अपने पद और प्रतिष्ठा को पहचानना चाहिए। समस्या या मामला कोई भी हो उसमें तुम्हारे वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से उल्लेख करते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आसानी पैदा करो, सख़्ती न करो। और शुभ सूचना दो, नफ़रत न दिलाओ।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : एक हदीस के मूलपाठ में ‘बश्शिरू’ (शुभ सूचना दो) के स्थान पर ‘सक्किनू’ (सुकून पहुँचाओ) का शब्द आया है। अभिप्राय ‘सक्किनू बिलबशारत’ ही है। अर्थात शुभ सूचना के द्वारा उन्हें सुकून पहुँचाओ।
एक हदीस में है कि हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) को यमन की ओर भेजते हुए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा था—
“आसानी पैदा करना, सख़्ती और दुश्वारी पैदा न करना। शुभ सूचना देना, नफ़रत न दिलाना, और आदेश में सहमति का ध्यान रखना, विभेद में न पड़ना।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
इन हदीसों से भली-भाँति अन्दाज़ा किया जा सकता है कि उम्मत की सुविधा का नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कितना अधिक ध्यान रखते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षा यह थी कि आज्ञापालन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए ताकि आज्ञापालन लोगों के लिए आसान हो जाए। पुण्य और सवाब और दूसरी बरकतों का उल्लेख करके आज्ञापालन को उनके लिए एक अभीष्ट कार्य बना दिया जाए। धार्मिक आदेशों और दायित्वों को दुस्साध्य बनाकर कदापि न प्रस्तुत किया जाए कि लोगों के लिए वे अप्रिय हो जाएँ या उसे अपने लिए एक आपदा समझने लगें।
यहाँ यह भी दृष्टि में रहे कि यह केवल हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अबू मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही की बात नहीं है बल्कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब भी और जिस सहाबी को भी हाकिम बनाकर कहीं भेजते तो उन्हें यही शिक्षा देकर भेजते कि—
"शुभ सूचना दो, नफ़रत न दिलाओ। आसानी पैदा करो, सख़्ती न करो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
विशालहृदयता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुम्हारे किसी साथी की मृत्यु हो जाए तो उसे छोड़ दो और उसकी बुराई बयान न करो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात तुम्हारा साथी जब अपने प्रभु के पास जा चुका तो अच्छा-बुरा सब उसपर प्रकट हो चुका होगा। अब उसकी बुराइयों के वर्णन की कोई आवश्यकता बाक़ी नहीं रहती। किसी की बुराइयों की चर्चा तो उसके जीवन में भी सही नहीं है सिवाय इसके कि कोई अपरिहार्य आवश्यकता पड़ जाए। किसी के मरने के बाद और वह भी जो अपना साथी या सहचर रह चुका हो उसे बुराई के साथ याद करना बहुत ही छोटेपन की बात होगी।
(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने मृत्युप्राप्त लोगों के गुणों की चर्चा करो और उनकी बुराइयों की चर्चा से बचो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात अब जबकि मरनेवाले दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं रहे तो याद करने की चीज़ उनके गुण और विशेषताएँ हैं न कि उनके दुर्गुण। जानेवाले तो याद आएँगे ही। उन्हें याद करना उनका एक हक़ भी है। लेकिन यह भी उनका हक़ है कि जो लोग पर्दापोश हो गए हों तुम उनकी पर्दादरी न करो। उनके दोष तुम्हारे मुख या क़लम से लोगों के सामने न आएँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो चाहे वे अच्छे रहे हों या न रहे हों लेकिन तुम्हें तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस्लाम जिस क्षमाशीलता और विशालहृदयता की शिक्षा देता है वह यह है कि तुम लोगों के अवगुणों को उछालने से बचो। दुष्प्रचार का माध्यम बनने के बजाय सुरुचिसम्पन्नता की बात यह होगी कि तुम्हारे द्वारा बुराई के स्थान पर भलाई को बल मिले।
मध्यमार्ग
(1) हज़रत सहल-बिन-साद साइदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कार्य को शान्ति और शालीनता के साथ करना अल्लाह की ओर से है और जल्दबाज़ी का सम्बन्ध शैतान से है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : एक हदीस में यह भी आया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छा चरित्र और गरिमा और शान्ति के साथ कार्य सम्पन्न करने की आदत और मध्यमार्ग नुबूवत के चौबीस भागों में से एक भाग है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
इन कथनों से शालीनता, गम्भीरता और मध्यमार्ग का महत्व भली-भाँति प्रकट होता है। इनसे यह भी ज्ञात हुआ कि ये गुण पैग़म्बराना जीवन की विशिष्टताएँ हैं। इनसे वंचित होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वे शीलगुण हैं जिनकी शिक्षा नबियों ने दी है। इसके विपरीत जल्दबाज़ी या वह अन्दाज़ जो गरिमा और शालीनता के विरुद्ध हो अप्रशंसनीय है। इससे यही नहीं कि आदमी के व्यक्तित्व को आघात पहुँचता है बल्कि इससे धर्म की भी कोई वास्तविक सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए कि धर्म को हानि पहुँचाकर धर्म की सेवा एक हास्यास्पद बात होगी।
यह जो कहा गया कि “कार्य को शान्ति और शालीनता के साथ करना अल्लाह की ओर से है और जल्दबाज़ी का सम्बन्ध शैतान से है” इससे कई चीज़ों को दिल-दिमाग़ में बिठाना अभीष्ट है। किसी चीज़ के ईश्वर की ओर से होने का अर्थ यह है कि ईश्वर उसे पसन्द करता है। और उसे धारण करना ईश्वरीय सहायता ही से सम्भव है। उसे धारण करने से बन्दा ईश्वर से बहुत निकट हो जाता है और शैतान के दायरे से बाहर निकल आता है। सुशीलता और वे गुण जिनकी शिक्षा इस्लाम ने दी है वास्तव में ईश्वरीय गुणों की प्रतिछाया हैं। ईश्वर चाहता है कि उसके गुणों का प्रतिबिम्ब उसके बन्दों पर पड़े ताकि उनके जीवन पवित्र और रश्मित हो सकें।
इसके विपरीत अप्रशंसनीय स्वभाव और दुराचरण का सम्बन्ध शैतान से होता है। उदाहरणार्थ यहाँ हदीस में जल्दबाज़ी के बारे में कहा गया कि वह शैतान की ओर से होती है। शैतान चाहता है कि इनसान जल्दबाज़ सिद्ध हो। वह गम्भीरता से किसी चीज़ के विषय में सोच-विचार न करे और न किसी चीज़ के परिणाम को देखे। बस मनेच्छाएँ उसकी पथप्रदर्शक हों। यह आतुरता और जल्दबाज़ी किसी सभ्यता का लक्षण नहीं हो सकती और इसके जो घातक परिणाम हो सकते हैं उनसे हम सभी अवगत हैं। जल्दबाज़ी में आदमी एक काम कर गुज़रता है और फिर उसके बुरे परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं। समय गुज़र चुका होता है। क्षतिपूर्ति का कोई उपाय शेष नहीं रहता।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन चीज़ें मुक्तिदायक हैं और तीन चीज़ें घातक हैं। जो चीज़ें मुक्तिदायक हैं वे ये हैं— छिपे और खुले हर हाल में अल्लाह से डरते रहना, प्रसन्नता हो या अप्रसन्नता दोनों हालतों में हक़ बात कहना और सम्पन्नता हो या निर्धनता दोनों स्थितियों में मध्यमार्ग अपनाना। और रहीं घातक चीज़ें तो वे ये हैं— मनेच्छा जिसका अनुसरण किया जाए और लोभ व कृपणता जिसका कोई ग़ुलाम बन जाए, और ख़ुदपसन्दी और आत्मप्रशंसा जिसमें कोई व्यक्ति ग्रस्त हो, और ये इन सबमें निकृष्टतम दुर्गुण है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअबिल ईमान)
व्याख्या : इस हदीस में यह बताया गया है कि मुक्तिदायक चीज़ें क्या हैं। अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता की अपेक्षा आदमी सत्य को महत्व दे। किसी से ख़ुश हो तब भी बात वही कहे जो हक़ हो भले ही वह बात उस व्यक्ति के विरुद्ध हो जिससे वह प्रसन्न है। इसी प्रकार उस समय भी वह हक़ बात कहने से विचलित न हो जबकि वह किसी से अप्रसन्न हो। चाहे उसके हक़ बात कहने से उस व्यक्ति को लाभ पहुँच रहा हो जिससे वह अप्रसन्न और नाख़ुश है।
ख़र्च करने में मध्यमार्ग का ख़्याल रखे। ख़र्च करने में न अपव्ययी हो और न कृपण हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि निर्धनता और तंगी की हालत में आदमी न तो अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचने दे और न सम्पन्नता में घमंडी और सरकश और वक़्त का फ़िरऔन बनने की कोशिश करे। वह प्रत्येक स्थिति में वही नीति अपनाए जिसे अल्लाह ने उसके लिए पसन्द किया है। और वह नीति यह है कि आदमी जीवन में मध्यमार्ग की कभी उपेक्षा न करे।
मुक्तिदायक चीज़ों के सम्बन्ध में मन को हमेशा सत्य के अधीन रखने की आवश्यकता होती है। अगर मन को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो आदमी की हलाकत और विशेषकर उसकी आख़िरत की तबाही और नाकामी निश्चित है।
हलाकत से बचने के लिए आवश्यक है कि आदमी स्वभावतः लोभ और कृपणता से मुक्त हो, यह आसान बात नहीं है। लेकिन वह यह तो कर ही सकता है कि लोभ और कृपणता को व्यवहार में न लाए, इसके विपरीत व्यावहारिक जीवन में अपने लिए उदारता को पसन्द करे।
हलाकत से सुरक्षित रहने के लिए अति आवश्यक है कि आदमी आत्मप्रशंसा से अपने आप को सुरक्षित रखे। आत्मप्रशंसा और ख़ुदपसन्दी निकृष्टतम वृत्ति है। अपने परिणामों और हानियों की दृष्टि से भी, और इस दृष्टि से भी यह निकृष्टतम रोग है कि ईश्वर की दृष्टि में सबसे ज़्यादा बुरा और अप्रिय व्यक्ति वह है जो अहंकारी और आत्मश्लाघी हो। इससे हटकर दूसरे गुनाहों में तो इसकी उम्मीद की जाती है कि आदमी इससे बाज़ आ जाए और अपने व्यवहार को बदल ले लेकिन अहंकारी और आत्मश्लाघी व्यक्ति से इसकी आशा बहुत कम होती है कि वह इस अधमता से निकलने में सफल हो सकेगा जिसको वह उच्च समझ रहा है।
क्षमादान
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि मूसा-बिन-इमरान (अलैहिस्सलाम) ने पूछा कि ऐ मेरे रब, तेरे बन्दों में से कौन व्यक्ति तेरी दृष्टि में अधिक प्रतिष्ठित है? अल्लाह ने कहा, "वह व्यक्ति जो (बदला लेने की) सामर्थ्य रखने के बावजूद क्षमा कर दे।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : वास्तव में इनसान की हैसियत एक नैतिक अस्तित्व की है। उसकी पूर्णता का रहस्य नैतिकता की पूर्णता में निहित है। नैतिक रूप से वह जितना उच्च होगा ईश्वर की दृष्टि में भी वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित होगा और लोगों की नज़र में भी उसका उतना ही अधिक महत्व होगा और उतना ही अधिक लोगों के दिलों में उसके लिए आदर पाया जाएगा।
इस हदीस ने इस समस्या को भी हल कर दिया है कि आम जीवन में यह कैसे मालूम हो कि कौन व्यक्ति नैतिक दृष्टि से उच्च स्थान पर है। सामर्थ्य रखने और क़ाबू पाने के बाद भी अगर कोई उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है और प्रतिशोध नहीं लेता जिसने उसे कष्ट पहुँचाया है तो समझ लीजिए कि वह नैतिक दृष्टि से अत्यन्त उच्च और ईश्वर की दृष्टि में बहुत ही प्रतिष्ठित है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, सद्क़ा (दान) देने से कोई माल घटता नहीं और क्षमा कर देने से अल्लाह बन्दे की इज़्ज़त बढ़ाता है। और जो कोई व्यक्ति अल्लाह के लिए विनम्रता अपनाता है तो इसके कारण अल्लाह उसे उच्चता प्रदान करता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से पता चलता है कि मोमिन बन्दे की दृष्टि भौतिक दृष्टिकोण से बिलकुल भिन्न होती है। यहाँ न तो ख़र्च करने से माल में कोई कमी आती है और न क्षमा करने से इज़्ज़त को कोई बट्टा लगता है और न ही विनम्रता के कारण आबरू ख़ाक में मिलती है। बल्कि परिणाम इसके विपरीत निकलते हैं। सदक़ा समाज को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होता है। फिर समाज में अगर असन्तोष न पाया जाता हो तो इससे स्वयं सद्क़ा देनेवाले को लाभ पहुँचता है। उसके व्यापार और कारोबार में बढ़ोत्तरी होती है। इस प्रकार सदक़ा अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सम्पत्ति का रक्षक और उसके धन की वृद्धि का कारण सिद्ध होता है।
क्षमा से काम लेना एक उदार कर्म है। इससे आदमी के व्यक्तित्व में निखार आता है और वह अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मानव चरित्र में विनम्रता से भी सुन्दरता आती है। इससे चरित्र निखरते और सँवरते हैं और आदमी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बन जाता है। विनम्रता किसी को पस्ती में नहीं गिराती बल्कि उसे उच्च स्थान प्रदान करती है।
मन की पवित्रता
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि लोगों में सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रत्येक वह व्यक्ति जो 'मख़्मूमुलक़ल्ब' और ज़बान का बहुत ही सच्चा हो।” सहाबियों ने कहा कि ज़बान का सच्चा तो हम समझ गए लेकिन मख़्मूमुलक़ल्ब हमारी समझ में नहीं आया, इसे स्पष्ट कर दें। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह वह स्वच्छ हृदय और ईश्वर से डरनेवाला व्यक्ति है जिसपर न तो गुनाह का बोझ हो और न अत्याचार और सीमोल्लंघन का, और न उसके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष हो और न इर्ष्या!” (हदीस : इब्ने-माजा, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : इस हदीस में आदर्श व्यक्ति का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त स्पष्ट और पूर्ण है। इसमें चरित्र के किसी पहलू की उपेक्षा नहीं की गई है। हृदय, जिह्वा और चरित्र, ये वे तत्व हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस हदीस में इन तीनों तत्वों के द्वारा मनुष्य का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें उसके बाह्य और अन्तर दोनों की पवित्रता और सौन्दर्य स्पष्ट है। ऐसे व्यक्ति के एक बेहतर इनसान होने में किसी व्यक्ति को भी सन्देह नहीं हो सकता।
ज़बान झूठ से अपरिचित और दिल हर प्रकार के द्वेष और मलिनता से मुक्त हो और चरित्र में कहीं अत्याचार और ज़्यादती का निशान मौजूद न हो तो आदमी के व्यक्तित्व में जो सौन्दर्य और आकर्षण उत्पन्न होगा उसका अनुमान प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इस हदीस से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम को किस नैतिकता, आचरण और व्यक्तित्व के लोग अपेक्षित हैं और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो समाज निर्मित होगा वह समाज कितना पवित्र होगा।
दूसरों की पद-प्रतिष्ठा का आदर
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं ने स्वप्न देखा कि मैं मिस्वाक (दातून) कर रहा हूँ। मेरे पास दो आदमी आए जिनमें से एक व्यक्ति दूसरे से (उम्र में) बड़ा था। उनमें जो छोटा था मैंने उसे मिस्वाक देने का इरादा किया तो मुझसे कहा गया कि मैं बड़े को दूँ। इसलिए मैंने मिस्वाक उनमें जो व्यक्ति बड़ा था उसे दे दी। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : "मुझसे कहा गया कि मैं बड़े को दे दूँ।" वह्य के द्वारा यह बात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कही गई।
ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों व्यक्ति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बाईं ओर थे। इस स्थिति में मिस्वाक का हक़दार वह व्यक्ति था जो दोनों में उम्र में बड़ा था। दूसरी स्थिति में प्राथमिकता इस बात को दी जाती कि जो व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दाईं ओर होता मिस्वाक उसी को दी जाए चाहे वह उम्र में दूसरे से छोटा ही क्यों न होता, जैसा कि एक अन्य हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दाईं ओर के लोगों को प्राथमिकता प्राप्त है। दाईं ओर के लोगों को प्राथमिकता प्राप्त है। ख़बरदार! अतः दाईं ओर वालों को दिया करो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
यह हदीस बताती है कि आदमी के स्थान और उसकी प्रतिष्ठा आदि को इस्लामी जीवन में कितना अधिक महत्व दिया गया है।
(2) हज़रत असमा बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ मेरे पास आई है और वह धर्म से विरक्त है। क्या मैं उसके साथ एहसान करूँ? रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हाँ"। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम में एक दूसरी हदीस से ज्ञात होता है कि यह उस समय की बात है जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और मक्का के क़ुरैश के मध्य सन्धि हुई थी और हज़रत असमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की माँ बहुदेववादी थीं। हज़रत असमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने पूछा, "मेरी माँ मेरे पास आई है और वह धर्म से विरक्त है तो क्या मैं उसके साथ एहसान करूँ।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हाँ, अपनी माँ के साथ एहसान करो।" (अर्थात सद्व्यवहार करो।)
मतलब यह कि बहुदेववादी होने के बावजूद और इसके बावजूद कि उसे सत्य-धर्म से घृणा है, वह तुम्हारी माँ है। उसके साथ सद्व्यवहार करना ही मानवीय आचरण के अनुकूल है। इस्लाम मानवीय नैतिकता को मिटाने नहीं, बल्कि उसे और अधिक सुदृढ़ करने आया है।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए घर की पली हुई बकरी का दूध दूहा गया, फिर उसमें उस कुँए का पानी मिलाया गया जो अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घर में था। फिर (दूध का) प्याला अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दिया गया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसमें से कुछ पिया। उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बाईं ओर हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे और दाईं ओर एक देहाती व्यक्ति था। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! (बचा हुआ दूध) अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को दें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे उस देहाती को दे दिया जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दाईं ओर था। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दाएँ को प्राथमिकता प्राप्त है। फिर दायाँ (अर्थात फिर जो उसके निकट हो)।”
एक रिवायत में ये शब्द आए हैं—
“दाईं ओर वालों को प्राथमिकता प्राप्त है, दाईं ओरवालों को प्राथमिकता प्राप्त है। सुन लो, अतएव दाईं ओरवालों को दिया करो।”
व्याख्या : हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग न करके अपना नाम ही ले लिया अन्यथा वे कह सकते थे कि उस दूध में उस कुँए का पानी मिलाया गया जो मेरे घर में था। बकरी भी हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घर में थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन ही के यहाँ पधारे थे।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि सर्वप्रथम उसको दिया जाए जो दाहिनी तरफ़ हो और फिर उस व्यक्ति को जो उसके पहलू में हो दिया जाए। और उसी ओर से और उसी क्रम के साथ चीज़ दी जाए यहाँ तक कि उस व्यक्ति तक नौबत पहुँचे जो बाईं ओर हो।
हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के निकटवर्ती होने और उनकी श्रेष्ठता के बावजूद और इसके बावजूद कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनके पक्ष में अपना मत भी व्यक्त किया, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने देहाती को प्राथमिकता दी इसलिए कि वह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दाईं ओर पड़ता था। इससे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के न्याय की पराकाष्ठा और सत्यप्रियता का पता चलता है।
दाईं ओर का अपना महत्व है। इसका यथासम्भव ध्यान रखना चाहिए। साधारणतः जीवन के इस तरह के मामले भी जो देखने में साधारण और छोटे मालूम होते हैं अपनी जगह महत्व रखते हैं। जो उन छोटे मामलों में न्यायप्रियता का सुबूत न दे उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़े मामलों में हक़ और न्याय पर क़ायम रह सकेगा। व्यक्ति का प्रशिक्षण वास्तव में जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों के द्वारा ही होता है।
ज़बान की सुरक्षा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते सुना—
“कभी-कभी बन्दा ऐसी बात ज़बान पर लाता है जिसके परिणाम पर वह विचार नहीं करता और उसके कारण वह फिसलकर नरक में जा पड़ता है हालाँकि वह उससे इतनी दूर होता है जितनी दूरी पूर्व और पश्चिम के मध्य पाई जाती है।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम में इस प्रकार आया है, “उसके कारण वह नरक में गिर जाता है उतनी दूरी से भी ज़्यादा दूरी से जितनी दूरी पूर्व और पश्चिम के मध्य पाई जाती है।" अर्थात वह नरक की आत्यान्तिक गहराई में जा पड़ता है।
मुख से अनुचित और अप्रिय बात कहने में कोई समय नहीं लगता लेकिन आदमी ईश्वर की नज़र से गिर जाता है और नरक के खड्डे में जा गिरता है। इससे मालूम हुआ कि उसकी यह भूल कोई मामूली भूल नहीं। इससे हम भली-भाँति समझ सकते हैं कि दुनिया में इनसान की स्थिति कितनी नाज़ुक है। ज़रा-सी असावधानी उसे तबाह और बरबाद करने के लिए पर्याप्त होती है। इनसान को ईश्वर ने जो प्रतिष्ठा प्रदान की है स्वभावतः उसे यह अपेक्षित है कि वह कोई ऐसा काम न करे यहाँ तक कि वह अपने मुख से कोई ऐसी बात निकालने को भी अनुचित समझे जो उसके मर्यादानुकूल न हो। अगर वह इस मामले में बेपरवाही से काम लेता है तो इससे स्वयं उसी को हानि पहुँचती है। चाहे उसे इसका शऊर और एहसास हो या न हो। यह बेशऊरी स्वयं एक गम्भीर अपराध है जो सत्य की दृष्टि में अक्षम्य है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कभी-कभी बन्दा ऐसी बात कहता है जिसके कहने से उसका उद्देश्य सिर्फ़ लोगों को हँसाना होता है। उसके कारण वह इतनी दूरी से (नरक में) गिरता है जितनी दूरी धरती और आकाश के मध्य पाई जाती है। और वह अपनी ज़बान के कारण उससे कहीं अधिक तीव्रता से फिसलता है जितना वह अपने पैर से फिसलता है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : अर्थात क़दम का फिसलना इतना अधिक आशंकापूर्ण नहीं होता जितना ज़बान का फिसलना आदमी के लिए घातक सिद्ध होता है। क़दम के फिसलने से आदमी धरती पर गिर सकता है। उसे शारीरिक चोट आ सकती है लेकिन ज़बान के फिसलने से आदमी का व्यक्तित्व ही आहत होकर रह जाता है, और हम किसी के लिए इससे बड़ी किसी हानि की कल्पना भी नहीं कर सकते।
A slip of the foot you may soon recover.
But a slip of the tongue you may never get over.
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो चुप रहा वह मुक्ति पा गया।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : अनगिनत फ़ितने एक ज़बान के कारण उठते हैं। यह ज़बान आदमी को नरक तक की सैर कराती है। आदमी औंधे मुँह नरक में गिरता है। कहा भी गया है—
"देहांग की दृष्टि से जिह्वा छोटी होती है लेकिन उसके अपराध और पाप भारी और बहुत होते हैं।"
झूठ, ग़लतबयानी और अनर्गल प्रलाप की तो धर्म में कोई गुंजाइश ही नहीं है लेकिन वे बातें जो लाभप्रद होती हैं उनमें भी दिखावा और कृत्रिमता आदि कितनी ही आपदाओं के मिश्रण की आशंका पाई जाती है। चुप रहना अगणित आपदाओं और विपत्तियों से आदमी को मुक्ति दिलाता है।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि सहाबियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक व्यक्ति ने (शव को सम्बोधित करते हुए) कहा कि तुझे स्वर्ग की शुभ सूचना हो। इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या तू यह बात कहता है और वास्तविकता से तू बिल्कुल अवगत नहीं। शायद उसने निरर्थक बात की हो या उस चीज़ में कृपणता दर्शाई हो जिसमें उसकी कोई हानि भी न थी।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस व्यक्ति को तू स्वर्ग की शुभ सूचना दे रहा है किसी मामले में उसकी पकड़ हो रही हो। और उसके स्वर्ग में जाने में कठिनाइयाँ और बाधाएँ उत्पन्न हो गई हों। यह बाधा कुफ़्र और शिर्क के कारण ही उत्पन्न नहीं होती बल्कि वे चीज़ें भी आदमी और उसके स्वर्ग के बीच बाधा बन सकती हैं जिनको लोग साधारण समझते हैं। क्या इसकी सम्भावना नहीं है कि उसने कुछ और नहीं तो निरर्थक और अनर्गल बातें ही की हों और ऐसे मामलों में कृपणता से काम लेकर अपनी संकीर्णता का परिचय दिया हो जिनमें कृपणता से काम लेने की सांसारिक दृष्टिकोण से भी कोई आवश्यकता नहीं होती, उदाहरणार्थ प्रसन्न मुद्रा में लोगों से मिलना, सलाम करना, सही मश्विरे देना या किसी को पानी पिला देना आदि। स्वर्ग तो अत्यन्त उच्च, विशाल और पवित्र स्थान है। उसमें किसी पस्ती, तंगी, अन्धकार और प्रदूषण के लिए कोई गुंजाइश कैसे निकल सकती है।
"उस चीज़ में कृपणता दर्शाई हो जिसमें उसकी कोई हानि भी न थी" का अर्थ यह भी हो सकता है कि उसने उस सद्क़े के देने में कृपणता दिखाई जो उसपर अनिवार्य था, जिसके देने से माल में बरकत ही होती, कमी नहीं होती जैसा कि क़ुरआन में है—
“और तुम जो कुछ भी ख़र्च करोगे वह (अल्लाह) उसका बदला देगा।" (34:39)
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
“सद्क़े से माल में कमी नहीं होती।" (हदीस : मुस्लिम)
(5) हज़रत सुफ़ियान-बिन-अब्दुल्लाह सक़फ़ी (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! जिनको आप मेरे लिए सबसे बढ़कर भय की चीज़ समझते हैं उनमें सर्वाधिक भयावह कौन-सी चीज़ है? हज़रत सुफ़ियान (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी ज़बान पकड़ी और कहा, “यह।”
ज़बान के ग़लत प्रयोग से जो फ़ितना और उपद्रव उत्पन्न होता है उसकी भयानकता से कौन इनकार कर सकता है। प्रत्येक वाक्य बल्कि प्रत्येक शब्द जो मुख से निकलता है अपने प्रभाव की दृष्टि से अमृत भी है और विष भी। यह वास्तव में उस व्यक्ति पर निर्भर है जो ज़बान से शब्द निकालता है। इसलिए आदमी को ज़बान के मामले में अत्यन्त सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यही शब्द हैं जो दिलों को जोड़ते भी हैं और दिलों को तोड़ते भी हैं। इनसानों को परस्पर मिलाने का काम भी करते हैं और उन्हें एक-दूसरे से दूर और विमुख भी करते हैं। ये रुलाते भी हैं और हँसाते भी हैं। इनसे भावनाओं को उत्तेजित करने का भी काम लिया जा सकता है और ये उत्तेजित भावनाओं को शान्त भी कर सकते हैं। कभी आदमी की ज़बान उसकी लेखनी होती है। नेपोलियन ने कहा है कि अगर बोरबन के सम्राट (Bourbon Kings) फ़्रांस के शक्तिशाली लेखकों को नियन्त्रण में रखते तो बोरबन राज्य (House of Bourbon) का ऐसा शिक्षाप्रद परिणाम कदापि न होता।
शब्दों का प्रभाव सर्वमान्य है चाहे वे ज़बान से निकलें या क़लम के द्वारा काग़ज़ पर प्रकट हों। शब्दों का ग़लत प्रयोग किसी अत्याचार से कम नहीं है। उससे बड़ा अपराधी और कौन होगा जो ईश्वर-प्रदत्त शक्ति को ईश्वरीय मंशा के विरुद्ध प्रयोग करके ईश्वर के बन्दों को किसी फ़ितने में डाल दे और सुधार के बजाय मानव समाज को उपद्रव और बिगाड़ से भर दे।
हमारी वाणी हमारे अन्तर्मन की सबसे बड़ी सूचक है। हमारे शब्द बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। एक वाक्य जो बेख़याली में भी मुख से निकलता है वह हमारे चेतन या अचेतन का परिचायक होता है। हदीस से मालूम होता है कि बहुधा हम अपने शब्दों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और वे हमें महान व्यक्तियों की श्रेणी में रख रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बुरी बात जो हमारे मुख से निकल रही होती है और हमें उसकी बुराई का आभास भी नहीं होता या हम उसे एक हल्की और साधारण बात समझ रहे होते हैं वास्तव में वही इसके लिए पर्याप्त होती है कि हमारी गणना निकृष्ट लोगों में हो। इससे भली-भाँति यह अनुमान किया जा सकता है कि ज़बान की ओर से हमें कितना सावधान रहना चाहिए।
यह समस्या तो भाषा और वार्तालाप की थी। इसी तरह आप कर्मों के विषय में भी सोच सकते हैं। बहुत सम्भव है कि एक कर्म जिसे हम कोई विशेष वज़न नहीं देते वह ईश्वर की प्रसन्नता का कारण बन जाए और एक कर्म जिसमें अपनी बेपरवाही के कारण हम कोई दोष महसूस न कर सकें वह हमें ईश्वरीय प्रकोप का भागी बना दे।
(6) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुस्लिम वह है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें। और मुहाजिर (वास्तव में) वह है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने रोका है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मुस्लिम होने के लिए आवश्यक है कि आदमी ईश्वर के अधिकारों के साथ-साथ उसके बन्दों के अधिकारों का भी लिहाज़ रखे। जीवन में बन्दों के हक़ को अदा करना वह विशिष्ट कसौटी है जिससे किसी भी व्यक्ति की ईमानी हालत का अन्दाज़ा होता है। जिस किसी व्यक्ति की ज़बान और हाथ से स्वयं उसके भाइयों की इज़्ज़त और उनकी सम्पत्ति आदि सुरक्षित न रहे वह सही अर्थों में मुस्लिम नहीं बन सका है, चाहे वह अपने मुसलमान होने की निहायत ज़ोर-शोर से घोषणा करता फिर रहा हो।
ईश्वर के धर्म के लिए घर-परिवार छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाने को हिजरत कहते हैं। मुहाजिर का धर्म में एक विशेष स्थान है। लेकिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इस हदीस से ज्ञात हुआ कि इस हिजरत के अतिरिक्त भी एक हिजरत है और वही वास्तविक हिजरत है। उस हिजरत में प्रकटतः न तो घर-बार छोड़ना पड़ता है और न कहीं स्थानान्तरित होना पड़ता है लेकिन वह एक महत्वपूर्ण हिजरत है। और वह है बुराइयों को छोड़ना और उन बातों को त्याग देना जिनसे ईश्वर ने रोका है। यह स्थान-परिवर्तन नहीं, चरित्र और व्यक्तित्व की क्रान्ति है। एक महान क्रान्ति!
(7) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अमुक स्त्री की नमाज़, उसके रोज़े और उसके सदक़े और ख़ैरात की बड़ी प्रसिद्धि है, मगर उसमें एक अवगुण भी है। वह अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से दुख पहुँचाती है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "वह नरक में है।" उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अमुक स्त्री के बारे में प्रसिद्ध है कि उसके यहाँ रोज़े, सद्क़े और नमाज़ की बहुलता नहीं, वह पनीर के कुछ टुकड़े सद्क़ा करती है लेकिन वह अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से कोई दुख नहीं पहुँचाती। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "वह स्वर्ग में है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : सामन्य दृष्टि में मूल महत्व नमाज़ और सद्क़ा अर्थात शारीरिक और धन सम्बन्धी इबादत का होता है। आम लोग व्यवहार, सदाचार और सामाजिक नियमों को विशेष महत्व नहीं देते। इस हदीस में एक बड़े भ्रम को दूर किया गया है। इबादत और पूजा परम स्वतन्त्र परमात्मा का हक़ है और सद्व्यवहार इनसानों का हक़ है जो मूलतः ज़रूरतमन्द हैं, और ज़रूरतमन्दों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनके निर्वाह के साथ-साथ ईश्वर के बन्दों के अधिकारों का लिहाज़ रखना भी अत्यावश्यक है। इसकी उपेक्षा अत्यन्त घातक है।
यहाँ एक बात और समझ लेने की है और वह यह कि नेकी चाहे कोई भी हो जब तक वह हमारे उत्कृष्ट चरित्र की परिचायक न हो सत्य की दृष्टि से उसका कोई वज़न नहीं है। यही कारण है कि वह स्त्री जो नमाज़ भी पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, सद्क़ा-ख़ैरात भी देती थी, उसको उसकी ये इबादतें नरक से न बचा सकीं। इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं कि इन इबादतों के बावजूद चरित्र की दृष्टि से वह कोई अच्छी स्त्री न थी। चरित्र और व्यक्तित्व का सम्बन्ध इनसान के सम्पूर्ण जीवन से होता है। इसलिए उत्तम और अभीष्ट चरित्र के गुण से आभूषित होने के लिए यह अनिवार्य है कि आदमी अपने जीवन के किसी भी हिस्से में बुरा सिद्ध न हो। उसे हम कहीं भी ज़ुल्म और ज़्यादती करते न पाएँ बल्कि वह प्रत्येक मामले में, चाहे उसका सम्बन्ध ईश्वर से हो या उसके बन्दों से, सत्य और न्याय पर क़ायम रहे। एक ओर वह ईश्वर का वफ़ादार हो तो दूसरी ओर ईश्वर के बन्दों का शुभचिन्तक और उनका कल्याण और भलाई चाहनेवाला हो। वह किसी के लिए कष्ट और दुख का कारण न बने।
(8) हज़रत अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदम का बेटा जब सुबह करता है तो शरीर के सारे अंग ज़बान के समक्ष याचना करते और कहते हैं कि हमारे मामले में ईश्वर से डर, क्योंकि हम तुझसे सम्बद्ध हैं। अगर तू ठीक रही तो हम भी ठीक रहेंगे और अगर तूने टेढ़ अपनाई तो हममें भी टेढ़ आ जाएगी।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात प्रत्येक सुबह को समस्त देहांग मूक भाव से ज़बान से यह याचना करते हैं कि तू ठीक रह और स्वच्छन्द न हो कि हम सब तेरे कारण मुसीबत में पड़ जाएँ।
एक हदीस में आया है कि समस्त देहांगों की दुरुस्ती हृदय की दुरुस्ती पर निर्भर करती है। अतः कहा गया है—
“जब हृदय ठीक रहता है तो सम्पूर्ण शरीर ठीक रहता है और जब वह बिगड़ता है तो सम्पूर्ण शरीर में बिगाड़ आ जाता है।"
इन दोनों बातों में तथ्यात्मक दृष्टि से कोई अन्तर्विरोध नहीं पाया जाता। मूल चीज़ तो हृदय है लेकिन प्रत्यक्ष में ज़बान उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दोनों ही के बारे में यह बात कही जा सकती है कि ये ठीक हैं तो सब ठीक हैं और अगर इनमें बिगाड़ आ गया तो फिर आदमी का संकटग्रस्त होना अनिवार्य है।
(9) हज़रत उक़बा-बिन-आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से भेंट की और पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपनी ज़बान पर क़ाबू रखो। और चाहिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में गुंजाइश हो और अपने गुनाहों पर रोया करो।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ज़बान आदमी के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। कोई आदमी क्या है? यह उसके कुछ बोल बता देते हैं। जिस प्रकार एक बीमार की आवाज़ बताती है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं उसी प्रकार आदमी की वाणी भी यह सूचित करती है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। आदमी का व्यक्तित्व उसके चित्र से कहीं अधिक उसकी वाणी से प्रकट होता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी ज़बान की ओर से आदमी ग़ाफ़िल न रहे। ज़बान को क़ाबू में रखे और निरर्थक चलने से उसे रोके। जैसा कि कहा गया कि आदमी अपनी वाणी के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है अगर वह ज़बान को अनुचित रूप से हर जगह प्रयोग करता है तो यह उसके सतही (निम्नस्तरीय) होने का स्पष्ट प्रमाण है। ज़बान की रक्षा में बड़ी हिक्मतें हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़बान पर नियन्त्रण रखता है तो यह संकेत है कि :
(i) वह सन्तुलित, धैर्यवान और सहनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति है।
(ii) इससे व्यक्तित्व के सौन्दर्य और गरिमा में वृद्धि होती है।
(iii) ऐसे व्यक्ति को सोचने, समझने और विचार करने के बहुमूल्य अवसर प्राप्त होते रहते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के दिल में तत्वज्ञान के स्रोत भी प्रवाहित हो सकते हैं।
(iv) दूसरों के अधिकारों का आदर करना उसके लिए दुष्कर न होगा। ज़बान पर अगर नियन्त्रण नहीं है तो आदमी अपनी ही कहे जाएगा। दूसरों को बोलने का अवसर न देगा। यह स्पष्टतः दूसरों के अधिकारों का हनन और उनके हृदयों को आहत करना है।
(v) ऐसा व्यक्ति परनिन्दा, अपशब्दों और व्यर्थ बातों से आसानी से बच सकेगा।
(vi) ऐसा व्यक्ति निरर्थक और अश्लील बातों के सुनने से भी बचेगा।
(vii) उसकी सारी ऊर्जा वाक्पटुता ही में व्यय न होकर चरित्र के निर्माण में लगेगी।
(viii) जब वह ज़बान पर नियन्त्रण रखेगा तो यही चीज़ उसे इस बात पर भी उभारेगी कि वह अपने दूसरे अंगों और अवयवों और ऊर्जा के प्रयोग में सावधान रहे।
यह हदीस बताती है कि ईमान की माँग केवल दिल की निगहबानी से ही पूरी नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आदमी अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को दृष्टि में रखे और उसे इस्लाम के साँचे में ढालने का प्रयास करे।
इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि आदमी सिरे से बात चीत ही न करे। हदीस की मंशा यह है कि आदमी अनावश्यक बात न करे, न ग़लत बात ज़बान पर लाए और न व्यर्थभाषिता और अतिभाषिता के रोग में ग्रस्त हो।
हम जो कुछ बोलते, पढ़ते और सुनते हैं उसका दिल पर प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव दिल पर अपनी ही बातों के द्वारा पड़ते हैं। आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण करते रहें। यह आत्मनिरीक्षण कर्मों और वचनों तक ही सीमित न हो बल्कि अपने हृदय का भी निरीक्षण करते रहें। हम यह देखते रहें कि हमारे हृदय की क्या दशा है। उसमें सही ईमानी भावों का विकास हो रहा है या नहीं। ईमानी भाव और माधुर्य मोमिन के लिए ईश्वर का तत्काल पुरस्कार और उपहार है।
इस हदीस से यह भी ज्ञात हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपने घर और सगे-सम्बन्धियों से कोई विशेष रुचि न हो। बाहर के कामों से निवृत्त हो तो अपने घर के काम-काज को भी देखो। और परिवारवालों की शिक्षा-दीक्षा की ओर ध्यान दो। अनावश्यक बाहर घूमते-फिरते रहने से कितनी ही बुराइयों और फ़ितनों के दरवाज़े खुलते हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए शान्तिगृह की हैसियत रखता है। इधर-उधर समय नष्ट करने का अर्थ इसके सिवा और क्या है कि तुम को घर के महत्व और मूल्य का एहसास नहीं है।
"अपने गुनाहों पर रोया करो" उत्तम शिक्षा है। मतलब यह है कि अपने गुनाहों पर नज़र डालो। विशेष रूप से अवकाश के समय अपनी कोताहियों और ग़लतियों पर निगाह डालो और ईश्वर के समक्ष आँसू बहाकर और विलाप करके उन्हें क्षमा कराने का प्रयास करो।
(10) हज़रत मुआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने (एक बार) निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे कोई ऐसा कर्म बता दें जो स्वर्ग में ले जाए और नरक से दूर रखे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुमने एक बहुत बड़ी बात पूछी है। मगर (बड़ी और भारी होने के बावजूद) वह उस व्यक्ति के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह उसको आसान कर दे। (और इसमें उसे ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो।) अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका साझीदार न बनाओ, और नमाज़ का आयोजन करो और ज़कात देते रहो और रमज़ान के रोज़े रखो और काबे का हज करो।" फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या मैं तुम्हें शुभ और भलाई के द्वार भी बता दूँ? रोज़ा ढाल है और सद्क़ा गुनाह (से पैदा होनेवाली आग) को इस प्रकार बुझा देता है जिस प्रकार पानी आग को बुझा देता है। और किसी व्यक्ति की वह नमाज़ जो वह मध्यरात्रि में अदा करे (अर्थात इसका भी यही हाल है। और नेकियों तथा भलाइयों के दरवाज़े खोलने में उसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।)" फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ‘त-तजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल-मज़ाजिइ का ... यअ'मलून तक पाठ किया। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या मैं तुम्हें धर्म का शीर्ष और स्तम्भ और उसका उच्च शिखर भी न बता दूँ?” हज़रत मुआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने कहा कि क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें अवश्य बताएँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “मूल आदेश तो इस्लाम है और उसका स्तम्भ नमाज़ और उसका उच्च शिखर जिहाद है।" फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बता दूँ जिसपर उनमें से प्रत्येक निर्भर करता है?" हज़रत मुआज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने कहा कि क्यों नहीं ऐ अल्लाह के नबी! आप अवश्य बताएँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी ज़बान पकड़ी और कहा, “इसको रोको।" मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! हम जो कुछ बोलते हैं क्या उसपर भी हमारी पकड़ होगी? कहा, "तुझे गुम करे तेरी माँ ऐ मुआज़! लोगों को नरक में उनके मुँह के बल या उनकी नाकों के बल इन ज़बानों की बेलगामियाँ ही गिराएँगी।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (क़ुरआन की) इन आयतों का पाठ किया—
“उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं कि वे अपने रब को भय और लालसा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। फिर कोई प्राणि नहीं जानता आँखों की जो ठंडक उसके लिए छिपा कर रखी गई है उसके बदले में देने के ध्येय से जो वे करते रहे होंगे।" (32:16-17)
इन आयतों से तहज्जुद की नमाज़ की श्रेष्ठता और महत्व भली-भाँति प्रकट होता है। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी बात की पुष्टि में इन आयतों की तिलावत की।
इस्लाम को धर्म का शीर्ष कहा गया है। आदमी के कर्म और उसकी नैतिकता देखने में कितनी ही ठीक क्यों न हों अगर इस्लाम पर उसका ईमान नहीं है तो फिर उसकी नैतिकता और सत्कर्मों की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे धड़ तो हो मगर सिर न हो। ऐसा धड़ चाहे वह कितना ही सुन्दर क्यों न हो किस काम का हो सकता है जो बेसिर का हो।
जिस धर्म की स्थापना इस्लाम में अपेक्षित है वह नमाज़ के बिना स्थापित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी भवन के लिए स्तम्भ दरकार होता है, क्योंकि स्तम्भ के बिना इमारत खड़ी नहीं होती, उसी प्रकार धर्म की इमारत भी निर्मित नहीं हो सकती और न खड़ी रह सकती है। जब तक कि नमाज़ का स्तम्भ उसके लिए उपलब्ध न किया जाए।
धर्म एक जीवन-व्यवस्था है। इस जीवन-व्यवस्था की मूल आत्मा तो एकेश्वरवाद और ईश्वर की बन्दगी है। नमाज़ वास्तव में ईश-वन्दना और ईशवर की चाहत ही का दूसरा नाम है। इस चाहत और दास्यभाव के बिना उस सत्य व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी ओर क़ुरआन ने दुनियावालों को आमन्त्रित किया है।
ईश-बोल को उँचा करना और सत्यधर्म की सर्वोच्चता चूँकि जिहाद पर निर्भर करती है इसी लिए जिहाद को उच्चतम शिखर कहा गया है।
इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि ये सारे ही कर्म अकारथ हैं अगर ज़बान की रक्षा न की गई। ज़बान के मामले में सावधानी कितनी आवश्यक है इसका अनुमान करने के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यही कथन पर्याप्त है। ज़बान पर नियन्त्रण रखने में अगर कोई व्यक्ति सफल हो गया तो इससे प्रत्येक उस आज्ञा के पालन की आशा की जा सकती है जिसकी शिक्षा इस्लाम ने अपने अनुयायियों को दी है। ज़बान के प्रयोग में असावधानी एक आम रोग है और इस रोग में जनसामान्य ही नहीं विशिष्ट लोग भी ग्रस्त दिखाई देते हैं।
“तुम्हें गुम करे तुम्हारी माँ" अरबी मुहावरे में ये प्रेम-प्रदर्शन के शब्द हैं। यह कोई बद्दुआ नहीं है।
यह हदीस बताती है कि ज़बान की रक्षा अत्यावश्यक है। अधिकांशतः लोग ज़बान की बेलगामियों के कारण नरक में डाले जाएँगे।
सुभाषिता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अच्छी और मीठी बात भी एक सदक़ा है।’’ (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यह एक लम्बी हदीस का हिस्सा है। बन्दों पर प्रतापवान और महान प्रभु के असीम उपकार हैं। सद्क़े के द्वारा बन्दा अपने प्रभु के उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करता है। सद्क़ा आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट साधन है। सद्क़ा और ख़ैरात करके आदमी ज़रूरतमंदों की मदद करता और उन्हें आराम पहुँचाता है। रुपये-पैसे से ही नहीं, अच्छी और उत्तम बातों से भी लोगों को फ़ायदे पहुँचते हैं। मृदुभाषिता से दिल हर्षित हो जाते हैं। इसलिए अच्छी और मीठी बातों को सद्क़े से अभिव्यंजित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक तथ्य है।
बात-चीत में शालीनता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ये सिद्दीक़ (सत्यवान) के मर्यादानुकूल नहीं कि वह ज़्यादा लानत करनेवाला हो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : 'सिद्दीक़ियत' (सत्यवादिता) एक ऊँचा स्थान है। सत्यवादियों का आचार नबियों के आचार के सदृश होता है। हम जानते हैं कि नबी दुनिया में रहमत बनकर आते हैं। उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं होती कि वे लोगों पर लानत करते फिरें। लोगों को ईश्वरीय अनुकम्पा से दूर फेंकना उनके लिए कोई प्रिय कार्य नहीं होता। उनकी सारी कोशिश यह होती है कि लोग सत्य से निकट और ईश्वरीय रहमत के आकांक्षी हों। नबियों (अलैहिस्सलाम) के इसी तरीक़े का अनुसरण करना सत्यवानों का कर्तव्य होता है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब कोई व्यक्ति कहे कि विनाश हुआ लोगों का, तो सबसे बढ़कर वह स्वयं विनष्ट होनेवाला है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : साधारणतः लोग एक प्रकार से ख़ुदपसन्दी और आत्मप्रशंसा में ग्रसित होते हैं। उन्हें स्वयं अपने अवगुण और कमज़ोरियाँ नज़र नहीं आतीं। वे दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। दूसरों की आँख का तिनका देखने में उनकी दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म होती है। लेकिन उनको अपनी आँख का शहतीर नहीं दीख पड़ता। वे वास्तव में ख़ुदपसन्दी और दंभ के ग्रास होते हैं। हालाँकि उन्हें लोगों के प्रति संवेदनशील और उनका हितैषी होना चाहिए था। उनका प्रयास तो यह होना चाहिए था कि लोगों को ईश्वरीय अनुकम्पा से निराश करने के बजाय उनके सुधार के लिए चिन्तित हों। लेकिन इसके विपरीत लोगों की लापरवाही पर दुख और रंज करने के बजाय उनको नारकीय घोषित करने ही में उनकी सारी दिलचस्पी होती है। ऐसी मानसिकता के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वे स्वयं सबसे बढ़कर विनष्ट होनेवाले हैं जिसका उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। अलबत्ता अगर धार्मिक मामलों में लोगों की बेपरवाही को देखते हुए चेतावनी स्वरूप किसी ने 'विनाश हुआ लोगों का' जैसी कोई बात कही तो उसके लिए यह डरावा नहीं है कि सबसे बढ़कर वह स्वयं विनष्ट होनेवाला है।
'सबसे बढ़कर वह स्वयं विनष्ट होनेवाला है' के स्थान पर 'तो उसने उन्हें विनष्ट किया' भी आया है। इस रूप में हदीस का अर्थ यह होगा कि यह कहकर कि लोगों का विनाश हुआ, आदमी उनका शुभचिन्तक नहीं बल्कि उन्हें निराश करके वास्तव में उन्हें विनष्ट करने का अपराधी बनता है। वह उन्हें निराश करके उनसे शौक़ और साहस और आज्ञाकारिता की भावना छीन लेना चाहता है। जबकि होना यह चाहिए कि जब हम लोगों को पापों में ग्रस्त देखें तो हिक्मत के साथ उन्हें ईश्वर के आज्ञापालन की ओर आमन्त्रित करें और उनके अन्दर आज्ञापालन और बन्दगी से लगाव और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने का शौक़ और उत्साह पैदा करें ताकि उनकी ग़फ़लत की निद्रा टूटे और वे ईश्वरीय अनुकम्पाओं के पात्र हो सकें।
शुद्ध वचन और पवित्र जीवन
(1) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। इसके बाद (वे या उनसे उल्लेख करनेवाले ने) एक लम्बी हदीस बयान की (जो यहाँ वर्णित नहीं)। इसी सिलसिले में बयान किया कि मैंने (हज़रत अबू-ज़र ने) अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे वसीयत और नसीहत करें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “मैं तुम्हें ईश-परायणता की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे सभी कामों को बहुत ही सँवारने और सुशोभित करनेवाली है।" मैंने कहा कि मुझे और भी नसीहत कीजिए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुम क़ुरआन की तिलावत और प्रतापवान ईश्वर के स्मरण को अपने लिए अनिवार्य कर लो। क्योंकि यह आसमान में तुम्हारी चर्चा का निमित्त होगा और धरती में तुम्हारे लिए प्रकाश बनेगा।" मैंने कहा कि आप मुझे कुछ और नसीहत कीजिए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अधिक ख़ामोश रहने को अपना स्वभाव बना लो, क्योंकि यह चीज़ शैतान को दूर करनेवाली और तुम्हारे धर्म के मामले में तुम्हारी सहायक होती है।" मैंने कहा कि आप मुझको और नसीहत कीजिए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ज़्यादा हँसने से बचो, क्योंकि यह चीज़ हृदय को मृतप्राय और मुख को निस्तेज कर देती है।" मैंने गुज़ारिश की कि आप मुझे और नसीहत करें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हक़ और सच्ची बात कहो, यद्यपि वह कटु हो।” मैंने निवेदन किया कि आप मुझे और भी नसीहत करें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अल्लाह के मामले में किसी धिक्कारनेवाले की धिक्कार की परवाह न करो।" मैंने कहा कि आप मुझको और भी नसीहत करें। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "जो कुछ तुम अपने विषय में जानते हो चाहिए कि वह तुम्हें लोगों के दोषान्वेषण से बाज़ रखे।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ-बिल ईमान)
व्याख्या : अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पहली वसीयत ईश-परायणता धारण करने और ईश्वर से डरते रहने की फ़रमाई और कहा कि ईशपरायणता तुम्हारे समस्त कर्मों को, चाहे उनका सम्बन्ध धर्म से हो या संसार से, सँवार देगी।
आदमी किसी न किसी काम में व्यस्त होता है, चाहे वह काम धर्म का हो या दुनिया का कोई काम हो। वह यह भी चाहता है कि उसे अपने कामों में सफलता प्राप्त हो। यहाँ बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईशपरायणता धारण करता है तो इससे उसके सारे ही काम बन जाएँगे। ईशपरायणता के लिए मूल में तक़वा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तक़वा भय और आदर या सजगता को कहते हैं। यह सबको मालूम है कि उत्तरदायित्व के बोध और सजगता के बिना कोई छोटे-से-छोटा कार्य भी सम्पन्न नहीं हो सकता। इसी लिए हर एक को व्यावहारिक जीवन में तक़वा का मार्ग अपनाना पड़ता है। व्यवसायी अपने व्यवसाय के लाभ और हानि को हमेशा अपने समक्ष रखता है। वह ऐसी युक्तियाँ अपनाता है जिससे कि उसके कारोबार में घाटा न हो बल्कि वह लाभ अर्जित कर सके।
ईमानवालों के यहाँ भी सजगता और उत्तरदायित्व को मौलिक महत्व प्राप्त है। अन्तर यदि है तो केवल यह कि सांसारिक और ईश्वर-विमुख लोग संसार ही को अपना अन्तिम लक्ष्य समझते हैं। वे बस प्रत्यक्ष को देखते हैं इसलिए कि उनके ज्ञान की पहुँच बस यहीं तक है, लेकिन ईमानवाले प्रत्यक्ष को ही नहीं बल्कि उसके पीछे कार्यरत मूल सत् पर भी नज़र रखते हैं। वे जानते हैं कि एक महान हस्ती इस चराचर जगत् को एक महान उद्देश्य के तहत चला रही है। वे इसको भी जानते हैं कि जिस प्रकार आज का एक कल भी है ठीक उसी प्रकार इस दुनिया की एक आख़िरत भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए ईमानवाले अपना सम्बन्ध केवल प्रत्यक्ष जगत् से ही स्थापित नहीं करते बल्कि वे अपना सम्बन्ध उस परोक्ष सत्ता से भी, बल्कि मूलतः उसी से, बनाए रखते हैं जो इस सृष्टि को एक सोद्देश्य चला रही है।
इस प्रकार मोमिनों और ग़ैर-मोमिनों के दृष्टिकोण में महान अन्तर पाया जाता है। ग़ैर-मोमिन केवल दुनिया के लिए जीता है। उसकी सारी भाग-दौड़ दुनिया के लिए होती है। ईमानवाले भी हालाँकि इसी दुनिया में बसते हैं और इसी वातावरण में साँस लेते हैं लेकिन उनका यहाँ जीना एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है। वे ईश्वर की मर्ज़ी के अधीन होते हैं और इस बात को भली-भाँति समझते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी का लिहाज़ रखना ही वह एकमात्र नीति है जिसके द्वारा अपने अधिकारों की भी रक्षा सम्भव है। अगर हम ईश्वर की मर्ज़ी के विरुद्ध चलते हैं तो यह विरोध केवल ईश्वरीय मंशा का न होगा बल्कि इस प्रकार हम स्वयं अपनी प्रकृति, जीवन की अर्थमयता और अपने भविष्य को भी तबाह कर लेंगे। और इसके बाद तो जिस चीज़ की प्रतीक्षा की जा सकती है वह चिरकालिक क्षोभ, निराशा और विनाश ही होगा।
एक दूसरे पहलू से भी इस बात को समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा ईश्वर है। प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व और स्थायित्व के लिए उसी पर निर्भर करती है। क़ुरआन में है—
"जिसने हर चीज़ को उसकी आकृति दी; फिर तद्नुकूल निर्देशन किया।" (20:50)
प्रत्येक चीज़ को ईश्वर ने आकृति और रंग-रूप दिया और वही उसे मार्ग पर भी लगाता है। चिड़ियों को पंख भी उसी ने दिए हैं और उन्हें उड़ना भी वही सिखाता है। मछलियों ने तैरना उसी से सीखा। उसका मार्गदर्शन न हो तो उपवन में फूल न खिल सकें और न ही धरती पर कहीं हमको हरियाली नज़र आए। फूलों की महक भी जाती रहे और बुलबुल का गीत भी हमेशा के लिए बन्द हो जाए। हमारे कामों में दुरुस्ती और हमारे व्यक्तित्व की पूर्णता भी ईश्वर की मर्ज़ी के पालन ही से सम्भव है। अगर ईश्वर की इच्छाओं का लिहाज़ रखा जाए तो इससे हमारे सांसारिक कार्य भी बन सकते हैं और आख़िरत का जीवन भी सँवर सकता है। ये दोनों ही चीज़ें हमें ईश्वर के आज्ञापालन से प्राप्त हो सकती हैं।
लेकिन सत्य से विमुख लोगों की नीति तो बस अत्याचार की होती है। वे ईश्वर से विमुख होकर जीवन के उद्देश्य की उपेक्षा करते हैं और मानव समाज को भी अत्याचार और उपद्रव से भर देते हैं जिसका ख़मियाज़ा अन्ततः उन्हें भी भुगतना पड़ता है। और आख़िरत में जिस दर्दनाक अंजाम से वे दोचार होंगे वह अपनी जगह एक बड़ी मुसीबत है जो किसी के टाले न टलेगी।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी दूसरी वसीयत में यह जो कहा कि "यह आसमान पर तुम्हारी चर्चा का निमित्त होगा और धरती पर तुम्हारे लिए प्रकाश बनेगा" तो वास्तव में इसमें क़ुरआन-पाठ और ईश-स्मरण के प्रभावों की ओर संकेत किया गया है। मालूम हुआ कि उच्चलोक का इहलोक से भी गहरा सम्बन्ध और सम्पर्क है। संसारवालों के मामलों के निर्णय वहाँ होते हैं। फ़रिश्तों का संसार में आना-जाना भी उच्च उद्देश्य के लिए होता है। फ़ज्र और अस्र के सिवा कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, उदाहरणार्थ शबे-क़द्र में फ़रिश्तों का अवतरण होता है। हमारे बारे में उच्चलोक अगर सन्तुष्ट है तो हम सुख-शान्ति से हैं, अन्यथा हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे चाँद पर उतरनेवालों से पृथ्वी पर लगातार सम्पर्क स्थापित रखा जाता है। पृथ्वी पर उनसे सम्पर्क रखनेवाले वैज्ञानिक अगर उनके बारे में सन्तुष्ट हैं तो समझा जाता है कि अन्तरिक्षयात्री शान्तिपूर्वक अपना सफ़र तय कर रहे हैं और वे किसी ख़तरे से दोचार नहीं हैं। उनकी सफलता और सुरक्षा सम्भावित है। विशेषज्ञों को जिस समय भी यह पता चलता है कि उन्हें कोई ख़तरा दरपेश है तो वे उनके लिए पृथ्वी से निर्देश प्रसारित करते हैं ताकि वे अपने आप को दरपेश ख़तरे से बाहर निकाल सकें। अब अगर वे इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं और पृथ्वी से अपने सम्बन्ध और सम्पर्क की परवाह नहीं करते तो उनका विनाश निश्चित है। ठीक यही स्थिति उच्चलोक से हमारे सम्बन्ध और सम्पर्क की है। हमारे चरित्र और कर्म के स्पष्ट प्रभावों का निरीक्षण उच्चलोक में किया जाता है। अगर आसमानी दुनिया में हमारे लिए निश्चिन्तता प्रकट की जाए और वहाँ हमारा ज़िक्र और प्रशंसा हो तो समझिए कि हम सलामती के मार्ग पर हैं अन्यथा हम तबाही और हलाकत की ओर बढ़ रहे हैं। हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह उच्चलोक में उन लोगों की चर्चा फ़रिश्तों की सभा में करता है जो दुनिया में ईश्वर को भूलते नहीं बल्कि उसे याद करते हैं। क़ुरआन में भी यह शुभ सूचना दी गई है—
"तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा।" (2: 152)
फिर यह ईश-स्मरण और क़ुरआन-पाठ बन्दे के लिए धरती में प्रकाश का कारण बनता है। यह प्रकाश मूलतः मोमिन के अन्तर में पैदा होता है। उसे एक पवित्र जीवन उपलब्ध हुआ है जो ईमानी भावों और आनन्द से परिपूर्ण और ईश-प्रसन्नताओं के अनुकूल होता है। ऐसा व्यक्ति उस परिन्दे की तरह जीवन नहीं गुज़ारता जो अपना आशियाना भूल गया हो और आकाश में इधर-उधर भटक रहा हो। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक मोड़ पर और जीवन की अच्छी-बुरी परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में समर्थ होता है। उसका निर्णय सही और ठीक होता है और वह समय पर सही क़दम उठाने की पोज़ीशन में होता है। ईश्वर की सहायता और अनुकम्पा भी उसके साथ होती है।
अपनी तीसरी वसीयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ज़्यादा ख़ामोश रहने पर ज़ोर दिया, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि ख़ामोशी मोमिन के लिए एक मज़बूत क़िला है जिसके कारण वह शैतानी हमलों से भी अपने आप को बचा सकता है और अपने दीन और ईमान की सरलतापूर्वक सुरक्षा भी कर सकता है।
व्यर्थभाषिता और अतिभाषिता आदमी को बेवज़न बना देती है। बहुधा ज़बान की बेबाकियों के कारण आदमी जहन्नम में गिर जाता है और उसे ख़बर भी नहीं होती। बेबाक इनसान शैतान को इसका पूरा अवसर देता है कि वह उसे अपने अपवित्र उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। अतिभाषी के लिए उन गुनाहों में पड़ने की आशंका ज़्यादा होती है जिनका सम्बन्ध आदमी की ज़बान से होता है। मिसाल के तौर पर झूठ, परनिन्दा और दुष्भाषिता आदि। अगर हम ख़ामोश रहते हैं तो हम बहुत-सी सांसारिक और धार्मिक आपदाओं से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और अपने धर्म की रक्षा की हमें ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। ज़्यादा ख़ामोश रहने का अभिप्राय यह नहीं है कि आदमी सिरे से मुँह ही न खोले। बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अनावश्यक बातों में अपना और दूसरों का समय नष्ट न करें। बोलें उस समय जबकि वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या फिर चुप रहे।" (हदीस : मुस्लिम)
ख़ामोशी इस दृष्टि से भी लाभप्रद और ज़रूरी है कि यह आदमी के लिए इसका अवसर देती है कि वह ईश्वर की निशानियों और उसकी दी हुई सुखकर वस्तुओं में सोच-विचार कर सके। ख़ामोशी से उसे इसका भी अवसर मिलता है कि वह ईमानी कैफ़ियतों को सुरक्षित रख सके और उन्हें विकसित भी कर सके।
यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की चौथी वसीयत थी कि ज़्यादा हँसने से बचो। ज़्यादा हँसी आदमी के हृदय को मृतप्राय कर देती है। अर्थात ज़्यादा हँसी-मज़ाक़ से हृदय संवेदनहीन और बेपरवाही का शिकार हो जाता है। वह एक प्रकार के अन्धकार से आच्छादित हो जाता है। जब हृदय निस्तेज हो गया तो चेहरा भी निस्तेज हो जाएगा। आदमी का मुख उसके हृदय के भावों को व्यक्त करता है। अतएव क़ुरआन में भी कहा गया है—
“वे अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं जिनपर सज्दों का प्रभाव है।" (49 : 29)
यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पाँचवीं वसीयत है कि हक़ बात कहने से कभी विचलित नहीं होना चाहिए चाहे वह बात स्वयं अपने या दूसरों के लिए अप्रिय और कटु ही क्यों न हो। ग़लतबयानी से काम लेकर आदमी अपने आप को असाधारण हानि पहुँचाता है। ग़लतबयानी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे उसके व्यक्तित्व को आघात पहुँचता है। यह ऐसी हानि है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी चीज़ से सम्भव नहीं है सिवाय इसके कि आदमी सच्चे दिल से तौबा करके अपने को सुधार ले।
यह छठी वसीयत है कि ज्ञानवान व्यक्ति को ईश्वर के मामले में किसी की परवाह नहीं होगी। वह वही कहेगा जो ईश्वर को प्रिय है और अपने लिए वह उसी मार्ग को चुनेगा जिसपर चलकर ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। किसी की प्रसन्नता के लिए वह अपने रब को कदापि अप्रसन्न नहीं कर सकता।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सातवीं वसीयत भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किस व्यक्ति को अपने अवगुणों और गुनाहों की ख़बर नहीं होती। उसे अपने को अवगुणों से मुक्त रखने का इतना प्रयास करना चाहिए कि दूसरों के अवगुण और दोष ढूँढने के लिए अवकाश ही न मिल सके। जो व्यक्ति भी आत्मनिरीक्षण करता रहेगा उसे अपने अन्दर इतनी ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ दिखाई देंगी कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालते हुए उसे शर्म आएगी और वह इससे बचेगा।
लोगों के दुखों और परेशानियों का ख़याल
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईमान की शाखाएँ सत्तर से कुछ ऊपर हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ इसकी स्वीकारोक्ति है कि अल्लाह के सिवा कोई प्रभु पूज्य नहीं, और सबसे कम दर्जे की शाखा किसी कष्टदायक वस्तु को रास्ते से हटा देना है। और लज्जा भी ईमान की एक शाखा है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईमान की शाखाएँ और उसकी अपेक्षाएँ बहुत-सी हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ यह स्वीकारोक्ति है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। वास्तव में यही ईमान की जड़ भी है। एकेश्वरवाद पर यक़ीन और ईमान अगर प्राप्त न हो तो इनसान के समस्त कर्म और उसकी समस्त नेकियाँ निष्प्राण और निरर्थक होकर रह जाएँगी। यह एकेश्वरवाद की धारणा ही है जो हमारे कर्मों को भरोसे के योग्य और मूल्यवान बनाती है। एकेश्वरवाद के बिना इनसान के चरित्र में न उच्चता और दृढ़ता आ सकती है और न ही उसमें वह सौन्दर्य और आकर्षण पैदा हो सकता है जिसकी सदा से मानव कामना करता रहा है।
इस हदीस में ईमान की अन्तिम शाखा इसको क़रार दिया गया है कि मार्ग से कष्टदायक चीज़ों को हटा दिया जाए ताकि किसी राह चलनेवाले को कोई तकलीफ़ या नुक़सान न पहुँचे। इसी प्रकार लज्जा और शर्म को भी ईमान की एक शाखा बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम का सम्बन्ध केवल धारणाओं से ही नहीं है बल्कि वह इनसान के कर्म और आचार और इससे भी आगे बढ़कर इनसान की सुरुचि और उसकी वृत्तियों तक को निखारने और सँवारने की योजना रखता है।
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"हर मनुष्य के शरीर में तीन सौ साठ जोड़ बनाए गए हैं। हर जोड़ एक सदक़ा या आभार व्यक्त करने की माँग करता है। तो जिस किसी ने अल्लाहु अकबर, अलहम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह और अस्तग़-फ़िरुल्लाह (अल्लाह सबसे बड़ा है, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, अल्लाह महान है, मैं अल्लाह से क्षमादान की प्रार्थना करता हूँ।) कहा और रास्ते से कोई पत्थर, काँटा, या हड्डी हटा दी या भलाई का आदेश दिया या बुराई से रोका, इस प्रकार तीन सौ साठ की गिनती के अनुसार सुकर्म कर लिए तो वह उस दिन इस दशा में चलता-फिरता होगा कि स्वयं को वह नरक की आग से दूर कर चुका होगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में एक तरफ़ इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि मनुष्य पर ईश्वर के असीम उपकार हैं जिनका उसे एहसास होना चाहिए और संसार में उसे कृतज्ञ बन्दा बनकर जीवनयापन करना चाहिए। कृतघ्न और काफ़िर बन्दा बनकर जीवनयापन करना उसके लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता।
दूसरी तरफ़ यह हदीस बताती है कि इनसान ईश्वर के उपकारों का शुक्र किस तरह अदा कर सकता है और इस सम्बन्ध में उसके लिए कितनी कुशादगी रखी गई है। अतएव बताया गया है कि ईश-स्मरण अर्थात तकबीर, तसबीह और तहमीद (अल्लाह की बड़ाई उसकी महानता का वर्णन और उसकी प्रशंसा) ही नहीं बल्कि हर नेक काम जो बन्दा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अंजाम देगा वह उसके कृतज्ञता प्रदर्शन में गिना जाएगा। अगर इनसान के जिस्म में तीन सौ साठ जोड़ हैं तो उनमें से प्रत्येक जोड़ ईश्वर का एक एहसान है जो उसने अपने बन्दे पर किया है। शरीर के जोड़ों में से कोई एक जोड़ भी कम हो जाए तो इनसान कठिनाई में पड़ जाए। अब इन तीन सौ साठ मेहरबानियों के जवाब में हम अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन इसी तरह कर सकते हैं कि एक ओर तो हम अपने मुख से ईश्वर की प्रशंसा और उसकी महानता का वर्णन कर रहे हों और हम उसके आगे नतमस्तक हों और दूसरी ओर व्यावहारिक जीवन में हम प्रत्येक अवसर पर कोई न कोई भलाई का काम करते रहें। लोगों को तबाही और बरबादी से बचाने के लिए प्रयासरत रहें। उन्हें नेकी और भलाई का आमन्त्रण दें। बुराइयों से उन्हें बाज़ रखने का प्रयास करें। हमें यह भी सहन न हो कि रास्ते पर पत्थर के टुकड़े, काँटे वग़ैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहें जिनसे लोगों को कष्ट पहुँचे। इस प्रकार अगर हम ईश्वर के एहसानों का हक़ अदा करने की कोशिश करते रहें तो धरती में हमारे अस्तित्व की हैसियत मात्र मुक्ति के पात्र की नहीं बल्कि मुक्ति प्राप्त की होगी।
अध्याय-3
नैतिक गिरावट
(1)
अंतर्दृष्टि का लोप
संवेदनहीनता
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“पिछले नबियों की वाणी में से जो बात लोगों ने पाई है वह यह है कि जब तूने शर्म और हया (लज्जा) को उठाकर रख दिया तो अब जो चाहे कर।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात पिछले नबियों की वाणी में से जो बात लोगों तक पहुँची है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सका है और जो आज के युग में भी उतनी ही सच्ची और खरी है जितनी पहले थी वह यह है कि तुझपर जब इस सीमा तक बेहिसी छा गई है कि तूने शर्म और लिहाज़ को उठाकर रख दिया और बेशर्मी ओढ़ ली तो फिर शर्मनाक से शर्मनाक हरकतें करने में तुझे क्या संकोच हो सकता है। बुरे कामों से आदमी शर्म और हया के कारण भी बाज़ रहता है। जब हया ही न रही तो फिर तू जो भी शर्मनाक हरकतें करे, दृष्टिवानों के लिए इसमें विस्मय और आश्चर्य की कोई बात न होगी। लेकिन तेरी उच्छृंखलता अन्ततः तुझे ले डूबेगी और तू ईश्वर की पकड़ से कदापि न बच सकेगा।
यह हदीस बताती है कि विगत काल के नबियों ने भी लज्जा को महत्व दिया है। क्योंकि लज्जा बुराई से रोकती है। हया और शर्म के उठ जाने के बाद आदमी से शिष्टतापूर्ण व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। अगर लज्जा बाधक न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अधमता और नीचता के किस छोर तक जाकर दम लेगा।
(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वह व्यक्ति हममें से नहीं है जो बड़ों का आदर-सम्मान न करे और छोटों पर दया न दर्शाए और भलाई पर न उभारे और बुराई से न रोके।” (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अपने बड़ों का आदर और अपने छोटों पर दया और कृपा एक स्वाभाविक चीज़ है। इसी प्रकार आम लोगों को नेकी और भलाई की नसीहत करना और उन्हें बुराइयों की ओर न जाने देने का प्रयास भी एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब जो इतना मुर्दा हो चुका हो और उसका स्वभाव इतना विकृत हो चुका हो कि न उसके दिल में अपने बड़ों के लिए आदर की कोई भावना शेष हो और न उसका व्यवहार अपने छोटों के साथ प्रेमपूर्ण हो और न ही उसे लोगों की भलाई और बुराई की कोई चिन्ता हो, स्पष्ट है ऐसे व्यक्ति को धर्म और धर्मवालों से क्या लगाव हो सकता है। सत्यवादी तो वास्तव में वे लोग होते हैं जिनकी आत्मा जीवन्त होती है। जो अपने दायित्व को भली-भाँति समझते हैं। धर्म भी इसके सिवा और क्या है कि वह हमारी संवेदनहीनता को समाप्त करके हमें ईश्वर, उसके बन्दों और स्वयं हमारे अपने हक़ से हमें अवगत कराता है और हमसे इसकी माँग होती है कि हम इन सब हक़ों को अदा करने का प्रयास करें।
भ्रमग्रस्तता
(1) हज़रत अबू-क़िलाबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अबू-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अबू-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से या अबू-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अबू-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा कि तुमने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से ‘ज़-अ'मू' के बारे में क्या सुना है? उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना, “ज़-अ'मू आदमी का बहुत बुरा तकिया कलाम है जिसे वह अपनी बात चलाने का साधन बनाता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ज़-अ'मू का अर्थ होता है— लोगों ने कहा है, लोगों का कहना है, लोगों का अनुमान है। शब्दकोष में “ज़अम” शब्द कहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन ज़अम और कथन में अन्तर पाया जाता है। शब्द ज़अम ऐसे अवसर पर प्रयोग करते हैं जहाँ कथन के प्रामाणिक होने पर पूर्ण विश्वास प्राप्त न हो बल्कि उसके ग़लत होने की सम्भावना पाई जाती हो। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ज़-अ'मू (लोग कहते हैं) के शब्द को बुरा तकिया कलाम कहते हैं। आदमी को वह बात कहनी चाहिए जिसके प्रति वह आश्वस्त हो। अविश्वसनीय और अप्रामाणिक बात को फैलाना समाज में किसी फ़ितने का कारण बन सकता है। इससे शंकालु प्रवृत्ति को बल मिलता है। मन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। ग़लत क़िस्म की प्रवृत्तियों और शंकाओं को हरगिज़ पैदा नहीं होने देना चाहिए। जिस बात के विश्वस्त और सही होने के बारे में संशय हो, उसके कहने की आवश्यकता ही क्या है? फिर ज़अम को लोगों पर थोपने से उनकी मानहीनता भी होती है।
इब्ने-कुतैबा ने 'मुख़्तलफ़ुल-हदीस' में और इमाम तहावी ने 'मुश्किलुल-आसार' में इस हदीस पर विस्तृत चर्चा की है। इस बहस का निष्कर्ष यह है कि जब तक किसी बात का पूरा विश्वास न हो जाए उसको फैलाना सही नहीं। झूठ से बचने के लिए उसे लोगों से जोड़कर बयान करना काफ़ी नहीं।
इस हदीस में अबू-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से अभिप्रेत हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं।
दिखावा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि अल्लाह कहता है—
"मैं समस्त साझीदारों में सबसे अधिक साझेदारी से निरपेक्ष हूँ। जो व्यक्ति कोई कर्म करता है और उसमें मेरे साथ किसी अन्य को साझीदार ठहराता है तो मैं उसको उसके साझीदार के साथ छोड़ देता हूँ।" एक रिवायत में है कि "मैं उससे विरक्त हूँ। वह उसी के लिए है जिसके लिए उसने किया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह कि दूसरे तो चाहे-अनचाहे साझेदारी को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन मुझे (अल्लाह को) यह स्वीकार नहीं कि कोई तनिक भी मेरा (अल्लाह का) साझीदार हो। एक व्यक्ति अगर कोई नेक कर्म करता है और इससे उसका प्रयोजन मेरी प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ और भी है, अर्थात वह इसके द्वारा दूसरों की सहमति और प्रसन्नता भी चाहता है तो मैं उससे और उसके इस मिश्रित कर्म से विरक्त हूँ।
अर्थात वह कर्म मेरे लिए नहीं है। मेरे यहाँ वही और केवल यही कर्म स्वीकृत होता है जो मेरी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए किया गया हो। मैं ऐसे कर्म से पूर्णतः विरक्त हूँ। वह व्यक्ति अपने ऐसे कर्म से किसी अन्य की प्रसन्नता प्राप्त करने में भले ही सफल हो जाए लेकिन उसे मेरी प्रसन्नता प्राप्त न होगी। मेरा स्वाभिमान और निरपेक्षता बहुदेववादी और मिश्रित कर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकती।
(2) हज़रत शद्दाद-बिन-औस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना—
“जिस किसी ने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया (अर्थात मेरा साझीदार बनाया), जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। और जिस किसी ने दिखावे के लिए सदक़ा किया उसने शिर्क किया।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : नमाज़, रोज़े और सदक़े का उल्लेख मात्र उदाहरण के लिए किया गया है। उद्देश्य यह है कि जो नेक कर्म भी दिखावे के साथ किया जाएगा वास्तव में वह एक प्रकार का बहुदेववादी कृत्य होगा। इसलिए कि जो कर्म उसे मात्र ईश्वर की बन्दगी और उसके आज्ञापालन की भावना से करना चाहिए था उसके करने में दूसरी ग़लत क़िस्म की भावनाएँ भी सम्मिलित हो गईं। यद्यपि यह बहुदेववाद वह प्रत्यक्ष बहुदेववाद नहीं है जिसके कारण आदमी सदैव के लिए नरक की यातना का पात्र हो जाता है लेकिन बहुदेववाद और कपटाचार के सदृश जो चीज़ भी होगी उसे अपनाने से आदमी उच्च स्थान से नीचे गिर जाता है। ईश्वर की महानता और उसकी प्रियता उसपर प्रकट नहीं होती। और मानव जीवन उच्च कोटि की भावनाओं से वंचित होकर रह जाता है। मानव की विनयशीलता में फिर कोई सौन्दर्य शेष नहीं रहता अगर वह ईश्वर की महानता को प्रत्यक्षतः न देखे। उसके हृदय की उत्कृष्ट भावनाएँ निरर्थक होकर रह जाती हैं यदि हृदय ईश्वर-प्रेम से रिक्त हो। प्रत्येक वह चीज़ जो हमें ईश्वर-विमुख करे हमारे लिए प्रतिमा है। (जिसकी पूजा एक घृणित कर्म है।) इसी लिए कहा भी गया है—
“प्रत्येक वह चीज़ जो तुझे ईश्वर से रोके वह तेरे लिए पूज्य प्रतिमा है।"
(3) हज़रत महमूद-बिन-लुबैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम्हारे बारे में सर्वाधिक भय मुझे सूक्ष्म बहुदेववाद का है।" लोगों ने पूछा कि सूक्ष्म बहुदेववाद क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “दिखावा।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि दिखावा कोई साधारण नैतिक रोग नहीं है जिसकी ओर से आदमी निश्चिन्त रहे। पाषाण-प्रतिमाओं की पूजा से बचना और उन्हें बेजान और तुच्छ समझना बहुत आसान बात है लेकिन आदमी दिखावे से दूर रहे, यह आसान नहीं है। आदमी साधारणतः अपनी मानसिक शान्ति के लिए भौतिक सहारे की तलाश करता है। दिखावा उसके लिए एक भौतिक सहारा होता है कि लोग उसे अच्छा समझेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और लोगों की दृष्टि में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। सत्कर्म का प्रेरक मात्र ईश-प्रसन्नता हो तो जीवन को अन्य प्रेरकों और मानसिक सहारों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ईश-प्रसन्न्ता की अभिलाषा हमें दूसरी चीज़ों से बेपरवाह बना दे यह उसी स्थिति में सम्भव है जबकि सही अर्थों में हमें अपने प्रभु की पहचान हो और ईश्वर हमें अपने जीवन में सम्मिलित दिखाई देने लगे। ईश्वर की उपस्थिति और उसके सर्वदर्शी होने का विश्वास ऐसा दिलों पर छा जाए और हृदय में ईश्वर की उपस्थिति से वह भाव जगे जो कभी लुप्त न हो।
(4) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे पास निकलकर आए। उस समय हम लोग आपस में मसीह दज्जाल की चर्चा कर रहे थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या मैं तुम्हें उस चीज़ की सूचना न दूँ जिसका मुझे तुम्हारे बारे में मसीह दज्जाल से बढ़कर भय है?” हमने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप अवश्य बताएँ। कहा, "वह सूक्ष्म बहुदेववाद है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति नमाज़ के लिए खड़ा हो, फिर वह अपनी नमाज़ इसलिए लम्बी कर दे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको (नमाज़ पढ़ते) देख रहा है।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : अर्थात मुझे इसका अधिक भय नहीं है कि दज्जाल खुले और स्पष्ट बहुदेववाद का आमन्त्रण लोगों को देगा और फ़ित्ना बनकर खड़ा होगा इसलिए कि सच्चे मोमिन कभी भी प्रत्यक्ष बहुदेववाद में ग्रस्त नहीं हो सकते। अलबत्ता मुझे इसकी आशंका अधिक है कि शैतान कहीं लोगों को सूक्ष्म प्रकार के बहुदेववाद में न ग्रसित कर दे, जिसकी एक मिसाल यह है कि आदमी किसी को दिखाने के लिए अपनी नमाज़ लम्बी कर दे और उसे अच्छे तरीक़े से अदा करने लगे। यह फ़ितना ऐसा है जिसका डर हर समय बना रहता है।
(5) हज़रत अबू-सईद-बिन-अबी-फ़ुज़ाला (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह क़ियामत के दिन, जिसके आने में कोई सन्देह नहीं, सब लोगों को एकत्र करेगा तो एक पुकारनेवाला पुकारेगा कि जिसने अपने किसी कर्म में, जिसे उसने अल्लाह के लिए किया, किसी अन्य को भी शरीक कर लिया तो उसे चाहिए कि वह उसका प्रतिदान अल्लाह के अतिरिक्त उसी अन्य से माँगे क्योंकि अल्लाह समस्त साझीदारों से अधिक बहुदेववाद के प्रति निरपेक्ष है।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर के यहाँ बहुदेववादी कर्म का कोई प्रतिदान कदापि नहीं मिलेगा। ईश्वर तो बस उसी कर्म को स्वीकार करता है जो केवल उसी की प्रसन्नता के लिए किया गया हो। क़ियामत के दिन घोषित कर दिया जाएगा कि जिस किसी के कर्म में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दूसरों की प्रसन्नता की चाह रही हो तो वह उन दूसरों से ही प्रतिदान का इच्छुक हो। ईश्वर के यहाँ ऐसे कर्म का कोई मूल्य नहीं है। यह उसकी शान से गिरी हुई बात है कि वह दूसरे साझीदारों के साथ किसी समझौते पर सहमत हो सके।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अन्तिम युग में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो धर्म को संसार-प्राप्ति का उपकरण बनाएँगे। वे लोगों को दिखाने के लिए भेड़ की खालें पहनेंगे। उनकी ज़बानें चीनी से भी ज़्यादा मधुर होंगी मगर उनके दिल भेड़ियों के दिल होंगे। अल्लाह कहता है कि क्या ये लोग मेरे ढील देने से धोका खा रहे हैं या (मुझसे निर्भय होकर) मेरे मुक़ाबले में दुस्साहस दिखा रहे हैं? अतः मुझे अपनी सौगन्ध, मैं अनिवार्यतः उनपर स्वयं उन्हीं में से ऐसा फ़ितना आरोपित कर दूँगा कि जो उनमें बुद्धिमान और ज्ञानवान को भी विस्मय में डाल देगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में अंतिम युग में प्रकट होने वाले एक बड़े फ़ितने की सूचना दी गई है जिसे हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि एक प्रकार का दिखावा और निकृष्टतम दिखावा यह है कि आदमी संयम और परहेज़गारी का ढोंग रचाए और इससे उसका प्रयोजन यह हो कि ईश्वर के भोले-भाले बन्दों को अपने जाल में फँसाकर उनसे दक्षिणाएँ आदि प्राप्त करके दुनिया कमाए। इस प्रकार के मक्कार और ऐयार लोगों से ईश्वर कठोर बदला लेने की धमकी देता है। वह उनको सख़्त फ़ितने में डाल देगा और उनके ज्ञानवान और बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी हैरान होकर रह जाएगी। उनकी समझ में न आएगा कि वे इस फ़ितने से कैसे छुटकारा प्राप्त करें।
(7) हज़रत ज़ुंदुब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने प्रसिद्धि की इच्छा की तो अल्लाह उसको प्रकट कर देगा और जो कोई दिखावे के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह उसे ख़ूब दिखाएगा।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात नेक अमल से अपनी प्रसिद्धि और नाम चाहनेवालों को ईश्वर उनके कर्म के अनुरूप यह दंड देगा कि उनके कपटाचार का भाँडा फूटकर रहेगा। जनसामान्य और विशिष्ट व्यक्तियों, सबपर यह खुल जाएगा कि उन्होंने अपने मन में क्या गन्दगियाँ छिपा रखी थीं। झूठी प्रसिद्धि चाहनेवालों को इस अपमान से भी पाला पड़ सकता है। क़ियामत के दिन उनके पाखंड का पर्दाफ़ाश तो होना ही है।
दिखावा वास्तव में ईश्वर और आख़िरत पर ईमान लाने की भावना का निषेध और शैतानी प्रवृत्तियों में से है। अतएव क़ुरआन में कहा गया है—
“और वे जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करते हैं, न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अन्तिम दिन पर, जिस किसी का साथी शैतान हुआ तो वह तो बहुत ही बुरा साथी है।" (4:38)
(8) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि उस व्यक्ति के बारे में आप का क्या विचार है जो कोई नेक कर्म करता है और उसके कारण लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एक रिवायत में है कि उसके कारण लोग उससे प्रेम करते हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यह तो मोमिन के लिए तात्कालिक शुभ सूचना है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इससे ज्ञात हुआ कि अगर कोई व्यक्ति नेक कर्म शुद्ध हृदय के साथ मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है लेकिन लोग उसकी नेकी के कारण उससे प्रेम करने लगते हैं या उसकी प्रशंसा करने लगते हैं तो इससे उसके नेक कर्मों के अकारथ होने की शंका नहीं करनी चाहिए। बल्कि इस प्रशंसा और प्रेम की हैसियत आख़िरत में मिलनेवाले प्रतिदान से पहले दुनिया में एक तात्कालिक और नक़्द पुरस्कार और उस व्यक्ति के स्वीकृत और प्रिय होने के एक लक्षण और पुर्व सूचना की होगी।
(9) हज़रत उस्मान-बिन-अफ़्फ़ान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी व्यक्ति की छिपी हुई अच्छी या बुरी कोई वृत्ति हो, अल्लाह उस (वृत्ति) से एक लक्षण दिखाता है जिसके द्वारा उसकी पहचान हो जाती है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : मूल में ‘रिदा’ शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अनुवाद यहाँ ‘लक्षण' किया गया है। रिदा चादर को कहते हैं। यहाँ इसका अभिप्राय लक्षण और सूक्ष्म एवं आत्मिक आकार-प्रकार से है। जिस प्रकार आदमी अपनी चादर से पहचान लिया जाता है उसी प्रकार आत्मिक आकार-प्रकार और लक्षण से भी आदमी की पहचान हो जाती है कि वह किस शील-स्वभाव और चरित्र का मनुष्य है। वास्तव में आदमी के कर्म और शील-स्वभाव का प्रभाव उसके व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होता है बल्कि आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण ही वास्तव में उसके आचार-व्यवहार से होता है। आचार-व्यवहार के प्रभाव एक सूक्ष्म रूप, आकार और आकृति धारण कर लेते हैं। यह रूप दृष्टि एवं हृदयाकर्षक भी हो सकता है और कुरूप और निस्तेज भी। यह इसपर निर्भर करता है कि उसके आचार-व्यवहार अच्छे हैं या बुरे। प्रत्येक हालत में आदमी अपने इसी सूक्ष्म रूप और आकार के द्वारा पहचान लिया जाता है कि वह कैसा है? विशेषकर उसका चेहरा उसके चरित्र की उच्चता और निम्नता और उसकी महानता और अधमता का द्योतक होता है। इसलिए आदमी का कर्म और चरित्र दृष्टिवानों से छिपा नहीं रह सकता। एक और हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कोई व्यक्ति किसी चट्टान के बीच कोई कर्म करे जिसमें न दरवाज़ा हो और न कोई रौशनदान हो तो भी उसका कर्म लोगों पर प्रकट होकर रहता है।" (अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
अर्थात किसी गुफा में छिपकर भी कोई कर्म किया जाए तो वह कर्म अपने प्रत्यावर्तन (Reflection) के द्वारा लोगों पर प्रकट हो जाता है।
दिखावे के द्वारा व्यक्ति जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है उसे वह चीज़ (वास्तविक इज़्ज़त) प्राप्त भी नहीं होती और उसके कर्म अलग अकारथ जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर के निष्ठावान बंदों के कर्म भी उनकी निष्ठा के कारण नष्ट नहीं होते और ईश्वर साधरणतः उनको नेकनामी और इज़्ज़त भी प्रदान करता है।
कपटाचार
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति में चार बातें पाई जाएँ वह कपटाचारी है। या जिस किसी में इन चारों में से कोई एक अवगुण पाया जाए तो उसमें कपटाचार का एक अवगुण मौजूद होगा, यहाँ तक कि वह उससे बाज़ आ जाए— जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसे पूरा न करे, जब प्रतिज्ञा करे तो उसे तोड़ डाले और जब झगड़ा करे तो बेक़ाबू होकर अश्लील बातों पर उतर आए।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : हदीस की किताब 'मुस्लिम' की एक रिवायत में 'मुनाफ़िक़न ख़ालिसन' (अर्थात निरा कपटाचारी) आया है।
मतलब यह है कि इस प्रकार के आचार-व्यवहार मोमिनों के नहीं, कपटाचारियों के हैं। कपटाचार का अर्थ ही यह होता है कि आदमी के आन्तरिक और बाह्य पक्षों में एकात्मता और समरसता न पाई जाए। आदमी बात तो ऐसी करे कि आभास हो कि वह सच कह रहा है। लेकिन वह झूठ से काम ले। वह वादा करके विश्वास तो यह दिलाए कि वह अपना वादा निभाएगा लेकिन वह अपने वादे का कुछ भी ख़याल न रखे। इसी प्रकार उसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में भी कुछ संकोच न हो और उसका किसी से झगड़ा हो तो मर्यादाओं का ध्यान न रखे। अशोभनीय हरकतें करने लगे और क्रोध में ऐसा अनियन्त्रित हो जाए कि बद-ज़बानी और दुर्वचनों से भी उसे कोई संकोच न हो। ये दुर्गुण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि ऐसा व्यक्ति विश्वासपात्र और भरोसे के योग्य नहीं है।
जिन गुनाहों का उल्लेख इस हदीस में किया गया है वे कपटाचारियों की घुट्टी में पड़े होते हैं। एक मुसलमान का दायित्व है कि वह कपटाचार के प्रत्येक लक्षण से विरक्त हो और उसे घृणायोग्य समझे। अपने जीवन को अन्तर्विरोध से मुक्त रखकर उसमें पूर्ण एकात्मता पैदा करे और कपटाचारियों के किसी अवगुण को अपने जीवन में कदापि प्रविष्ट न होने दे और अगर संयोगवश कोई गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन तौबा करके अपना सुधार करे।
अगर इन दुर्गुणों में से, जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है, कोई दुर्गुण किसी मुसलमान के अन्दर पाया जाता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसके अन्दर कपटाचार का एक लक्षण पाया जाता है। और अगर ये समस्त दुर्गुण उसके अन्दर व्याप्त हैं तो मानो वह पूर्णतः कपटाचारियों के समरूप हो गया है। उसकी यह नीति उसके ईमान और विश्वास के लिए अत्यन्त घातक है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कपटाचारी के लक्षण तीन हैं— जब बात करे तो झूठ बोले, जब वचन दे तो उसके विरुद्ध जाए, और जब उसपर भरोसा किया जाए तो विश्वासघात करे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : हदीस की किताब 'मुस्लिम' में ये शब्द भी मिलते हैं “यद्यपि वह रोज़ा रखता, नमाज़ पढ़ता और अपने मुसलमान होने का दावा करता हो।”
कपटाचार वास्तव में इनसान के आन्तरिक और बाह्य जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोध को कहते हैं। जिसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। लेकिन मूलतः उनके चार या तीन रूप होंगे। उपर्युक्त हदीस में कपटाचार के चार बुनियादी लक्षणों का उल्लेख किया गया है और इस हदीस में तीन बुनियादी लक्षण बताए गए हैं। इसकी भी सम्भावना पाई जाती है कि किसी विशेष चरण में चार या इससे भी अधिक लक्षणों को मौलिक स्थान दिया जाए। और किसी दूसरे चरण में किन्हीं तीन लक्षणों को मौलिक महत्व प्राप्त हो। एक हदीस में कपटाचारियों के आठ लक्षणों का उल्लेख किया गया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
"कपटाचारियों के कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा वे पहचाने जाते हैं : सलाम के बजाए उनके मुख पर सदैव लानत भरे शब्द होते हैं। उनका भोजन लूट का माल और उनका विजित धन (माले-ग़नीमत) विश्वासघात होता है। वे मस्जिदों में व्यस्त नहीं होते सिवाय इसके कि वहाँ ओछी बकवास करते हैं। नमाज़ में सिर्फ़ अन्त में सम्मिलित होते हैं। न वे स्वयं किसी से प्रेम करते हैं और न दूसरों को उनसे कोई प्रेम होता है। रात में शहतीर की भाँति बिस्तरों पर पड़े रहते हैं और दिन में शोर मचाते फिरते हैं।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित)
इस हदीस में कपटाचारियों का जो चित्रण किया गया है वह अत्यन्त सम्पूर्ण है। इससे उनकी नैतिक अवस्था और आर्थिक जीवन का पूरा चित्र सामने आ जाता है। यह हदीस बताती है कि नैतिकता की दृष्टि से कपटाचारी अत्यन्त गिरे हुए और पतित होते हैं। स्वार्थपरता उनका मूल स्वभाव होता है और विश्वासघात उनकी वृत्ति। धर्म से उनका कोई लगाव नहीं होता। जब धर्म का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं तो नमाज़ से उन्हें क्या रुचि हो सकती है। स्वार्थपरता और प्रेम में क्योंकि विरोध पाया जाता है इसलिए ये स्वार्थी किसी से प्रेम और अनुराग का सम्बन्ध नहीं रखते। दूसरे लोगों के दिलों में भी उनके लिए कोई प्रेम नहीं हो सकता। उनका प्रत्येक कर्म ईमान की अपेक्षाओं के विरुद्ध होता है इसलिए उनको मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) के नाम से पुकारा गया।
(3) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा और मितभाषिता एवं संकोच ईमान की दो शाखाएँ हैं और दुष्भाषिता और वाक्पटुता कपटाचार की दो शाखाएँ हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मोमिन चूँकि दायित्वपूर्ण जीवन व्यतीत करता है इसलिए वह जो कुछ भी कहता है सोच-समझकर कहता है। उसे पूरा एहसास होता है कि उसे अपने एक-एक शब्द का ईश्वर के सामने हिसाब देना है। इसलिए स्वभावतः वह निर्भयता और बेबाकी के साथ बात नहीं करता। फिर वह जो कुछ करता है उससे उसका उद्देश्य केवल ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना होता है। इसलिए वह किसी मजमे पर छा जाने और अपनी वाक्पटुता से लोगों पर धाक जमाने के चक्कर में नहीं रहता। वह आवश्यकता से अधिक बोलने के प्रयास से बचता है। फिर चूँकि वह लज्जाशील होता है और यह लज्जा उसे बाध्य करती है कि वह कोई ऐसा ढंग न अपनाए जो ईश्वर की दृष्टि में अप्रिय और दोषपूर्ण हो। वह लोगों के साथ निर्लज्ज व्यसनों में नहीं पड़ सकता, न वह लोगों के सामने डींगें मारता है और न उन्हें अपमानित करने में उसे कोई दिलचस्पी होती है। लेकिन वह सत्य को कभी छिपाता भी नहीं। अलबत्ता सत्य कहने में इसका ध्यान रखता है कि किसी का व्यर्थ ही दिल न दुखे। उसकी झिझक का एक बड़ा कारण उसकी लज्जा भी है। उसे अगर चिन्ता होती है तो इस बात की कि किसी प्रकार लोग सत्य से परिचित हो सकें और वे अपने प्रभु को पहचान लें।
कपटाचारी का मामला इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वह वार्तालाप और भाषण में वाक्पटुता दिखाना और लोगों पर रौब गाँठना चाहता है और अपने जादूई भाषण से लोगों को अपने चतुर्दिक एकत्र करना चाहता है। सत्य से वस्तुतः उसे कोई लगाव नहीं होता। इसलिए उसका सम्पूर्ण वक्तव्य तेजहीन और भावरहित होता है। ज़रा भी सोच-विचार से काम लिया जाए तो भली-भाँति उजागर होगा कि उसकी बातें सिर्फ़ बातें ही हैं जिनके पीछे कोई गहरा एहसास और सत्यज्ञान काम नहीं कर रहा है।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति इस दशा में मरा कि न तो उसने ईश्वरीय मार्ग में युद्ध किया और न कभी उसके दिल में इसका विचार ही आया तो उसकी मृत्यु कपटाचार की एक शाखा को लेकर हुई।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मोमिन की शान यह होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो ईश्वर के मार्ग में अपने प्राण तक न्योछावर करने से न चूके। और अगर इसका अवसर न उपलब्ध हो सके तो कम से कम इस आकांक्षा में उसका दिल तड़पता रहे कि काश मुझे ईश्वरीय मार्ग में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता।
इस्लाम में युद्ध स्वयं अपने आप में अपेक्षित नहीं है। इस्लाम ने धरती के उपद्रव की समाप्ति के लिए युद्ध की अनुमति दी है। इस्लाम में मूल उद्देश्य सत्य एवं न्याय व्यवस्था की स्थापना है। सत्य व्यवस्था की स्थापना के लिए असल काम यह है कि लोगों को ईश्वरीय धर्म की ओर आमन्त्रित किया जाए और सत्यवादियों को और उन लोगों को जो इस आमन्त्रण को स्वीकार करें संगठित व एकीकृत किया जाए और उन्हें एक सक्रिय शक्ति का रूप दिया जाए। इसलिए कि सामूहिक प्रयासों के बिना सत्य-व्यवस्था की स्थापना का स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता।
अब अगर कोई ईश्वरीय मार्ग में लड़ने की कामना तो करता है किन्तु आमन्त्रण सम्बन्धी प्रयासों और सत्य के उपासकों की एकता से उसे कोई लगाव नहीं है तो फिर या तो उसे सत्यधर्म और उसकी अपेक्षाओं का कोई ज्ञान नहीं है या फिर वह इस प्रकार से अपने आप को और ईश्वर को धोखा देना चाहता है।
(5) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कपटाचारी की मिसाल उस आवारा बकरी की-सी है, जो नर की तलाश में दो रेवड़ों के बीच कभी इस तरफ़ और कभी उस तरफ़ मारी-मारी फिरती हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में कपटाचार की मानसिकता को एक प्रभावी मिसाल के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कपटाचारियों को मात्र सांसारिक लाभ प्रिय होता है। उनकी दृष्टि केवल इसपर केंद्रित होती है कि अपनी जान और माल की सुरक्षा कैसे हो। उनके अन्दर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। वे केवल अपनी सुरक्षा की चिन्ता में पड़े होते हैं। चाहे यह सुरक्षा किसी के यहाँ भी मिल सके। उन्हें इसकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं होती कि यह सुरक्षा और निश्चिन्तता की चाहत संसार या परलोक कहीं का भी उन्हें न रहने देगी।
कथनी और करनी का अन्तर
(1) हज़रत उसामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“क़ियामत के दिन एक व्यक्ति को लाया जाएगा, फिर उसे नरक में डाल दिया जाएगा तो उसकी आँतें आग में निकल पड़ेंगी। वह इस प्रकार घूमेगा जिस प्रकार गधा अपनी चक्की के साथ घूमता है। नरकवाले उसके पास एकत्र हो जाएँगे और कहेंगे : ऐ अमुक व्यक्ति, यह तेरा क्या हाल है? क्या तू हमें अच्छी बातों का हुक्म नहीं देता था और बुरी बातों से हमें नहीं रोकता था? वह कहेगा कि मैं तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म तो देता था मगर उनपर स्वयं अमल नहीं करता था और तुम्हें बुरी बातों से तो रोकता था लेकिन स्वयं उनमें ग्रस्त रहता था।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : दूसरों को उपदेश देना और अपनी दुर्दशा से अनभिज्ञ रहने का यह कितना शिक्षाप्रद परिणाम होगा। कथनी और करनी के अन्तर से आदमी क़ियामत में सरेआम अपमानित होगा। नरक की कठोर यातना उसके हिस्से में आएगी सो अलग। वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति दूसरों को जगाने की चिन्ता में घुला जाता है और स्वयं ग़फ़लत ही में पड़ा रहना चाहता है उसकी यह नीति हास्यास्पद ही कही जाएगी। उसका वही अंजाम होना चाहिए जिसकी सूचना इस हदीस में दी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसे नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के सिलसिले में सबसे पहले अपनी चिन्ता हो और अपने सुधार की ओर से एक क्षण के लिए भी असावधान न हो।
इस हदीस में चित्रित किया गया है कि उस व्यक्ति की क़ियामत के दिन कैसी दुर्दशा होगी जो दूसरों को तो अच्छी बातें बताता है और उसे स्वयं अपने सुधार की चिन्ता नहीं होती। बताया जा रहा है कि नरक में आँतें निकल पड़ेंगी और वह इस प्रकार घूमेगा जिस प्रकार चक्की के चारों ओर वह जानवर, गधा हो या बैल, घूमता है जिससे चक्की को चलाने का काम लिया जाता है या जिस प्रकार हमारे यहाँ कोल्हू का बैल कोल्हू के चारों ओर घूमता है।
(2) हज़रत उमर-बिन-ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुझे इस उम्मत के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसे कपटाचारी से आशंका है जो बातें तो बुद्धिमानी की करता है लेकिन कर्म उसके अन्यायपूर्ण होते हैं।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : अर्थात ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वथा उपद्रव हैं जिनकी बातें अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण और विचारात्मक हों किन्तु उनके कर्म अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण हों। ये संकेत उन नेताओं की ओर भी हो सकता है जो धार्मिक सीमाओं का स्वयं सबसे अधिक उल्लंघन करते हैं। उनके मायाजाल से बचना आसान नहीं होता। इसलिए कि वे इस कला में इतने पारंगत और अद्वितीय होते हैं कि अपने व्याख्यानों और व्याख्याओं से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाएँ। इस प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा फ़ितना है। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस तरह के आदमी को उम्मत के लिए अस्ल ख़तरा बताते हुए उससे सावधान रहने का निर्देश दे रहे हैं।
भ्रममूलक बातों में डालना
(1) हज़रत सुफ़ियान-बिन-उसैद हज़रमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
"बड़ा विश्वासघात यह है कि तुम अपने भाई से ऐसी बात कहो जिसे वह सत्य समझे और तुम उससे झूठ कहो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि विश्वासघात का सम्बन्ध केवल धन-सम्पत्ति और अमानतों ही से नहीं है। अपनी ग़लत नीति से आदमी किसी भी मामले में अपने विश्वासघाती होने का प्रमाण दे सकता है। इस हदीस में एक मिसाल बात-चीत की दी गई है। अपनी बात-चीत में कोई व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। विश्वासघात वास्तव में एक प्रकार की धोखाधड़ी है। आदमी बात ऐसे अन्दाज़ से करे कि सुननेवाला उसे सच समझे जबकि वह झूठ हो तो यह भी विश्वासघात है, और बड़ा विश्वासघात है। अपने भाई को किसी धोखे में डालना किसी प्रकार उचित नहीं है।
इस हदीस से ज्ञात हुआ कि धर्म में अभीष्ट यह है कि मोमिन व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के अशुभ कृत्यों से विलग रहे और कभी भी कोई ऐसी नीति न अपनाए जिसमें कोई छल-कपट पाया जाता हो।
हदीस में शब्द ‘भाई’ प्रयुक्त हुआ है, जिससे अभिप्रेत हर इनसान है। इस्लाम की दृष्टि में तमाम इनसानों की हैसियत आपस में भाई की है। क्योंकि सारे ही इनसान एक माँ-बाप की सन्तान हैं।
अतिशयोक्ति
(1) हज़रत मुतरिफ़-बिन-अब्दुल्लाह-बिन-शिख़्ख़ीर कहते हैं कि मेरे पिता (अब्दुल्लाह) कहते हैं कि मैं बनू-आमिर के प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित होकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। हमने निवेदन किया कि आप हमारे सरदार और आक़ा हैं। कहा, “आक़ा तो अल्लाह है।" हमने निवेदन किया कि श्रेष्ठता की दृष्टि से आप हममें श्रेष्ठ हैं और बख़शिश की दृष्टि से आप हममें सबसे बढ़कर महान हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह बात कहो या इससे भी कुछ कम ही कहो और शैतान तुम्हें अपना वकील न बनाए।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : आक़ा और मालिक तो ईश्वर ही है। तमाम मामले वास्तव में उसी के हाथ में हैं। आक़ा और प्रभु कहलाने का वास्तव में अधिकारी वही है। हदीस के टीकाकारों का मत है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सम्बोधन का यह ढंग इसलिए पसन्द नहीं किया कि क़ौमों और क़बीलों के धनी और सरदारों को इसी प्रकार की उपाधि से लोग सम्मानित करते थे। प्रतिनिधिमंडल के लोगों के लिए उचित यह था कि वे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नबी और रसूल की उपाधि से याद करते। नुबूवत और रिसालत से बढ़कर किसी उच्च पद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रद्धा की भावना की तृप्ति का सामान भी इसमें सबसे बढ़कर था। यूँ तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नायकता और सरदारी तो सबपर प्रकट है। आप के कथन का सार यह है कि आम लोगों की भाँति अतिशयोक्ति से काम न लो। ऐसा न हो कि तुम ऐसी बातें कहने लग जाओ जिनसे गुमराही के रास्ते खुलते हैं। शैतान यही चाहता है कि लोग या तो रसूल पर ईमान ही न लाएँ और अगर लाएँ भी तो वे अपने रसूल के बारे में ऐसी अतिशयोक्ति करें कि उसे ईश्वरत्व के स्थान तक ले जाने में भी उन्हें कोई झिझक और संकोच न हो। ईसाइयों ने यही तो किया कि ईश्वर के नबी हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) को ईश्वर का बेटा बल्कि ईश्वर बनाकर छोड़ा और अधर्म और पथभ्रष्टता में बहुत दूर निकल गए।
झूठ
(1) हज़रत समुरा-बिन-जुन्दुब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल) ने कहा—
“स्वप्न में मैंने देखा कि दो व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जिसको आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (मेराज की रात्रि में) देखा था, उसके जबड़े चीरे जा रहे थे, वह बहुत बड़ा झूठा था। वह इस प्रकार की झूठी बातें उड़ाता था कि वे दुनिया में हर ओर फैल जाती थीं। उसके साथ क़ियामत तक ऐसा ही होता रहेगा।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : वह चूँकि झूठ बोलता था और जीभ और मुँह का ग़लत प्रयोग करके झूठी बातों को फैलाता था इसलिए उसके लिए जो दण्ड निर्धारित किया गया वह यह कि क़ियामत के दिन तक उसके जबड़े और कल्ले चीरे जाते रहेंगे। आख़िरत में जो दण्ड उसे मिलेगा वह अलग है।
इस हदीस से ज्ञात हुआ कि मरने के बाद से लेकर क़ियामत के दिन तक के लिए जबकि लोग ज़िन्दा करके उठाए जाएँगे, आदमी बिल्कुल फ़ना (विनष्ट) नहीं हो जाता बल्कि उसके अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा को अच्छी या बुरी अवस्था में रहना पड़ता है। मरने के बाद से लेकर क़ियामत तक का उसका यह जीवन 'बरज़ख़' का जीवन कहा जाता है। फिर इस हदीस से यह भी ज्ञात हुआ कि जीवन भौतिक शरीर के बिना भी सम्भव है बल्कि वास्तव में चेतना, वाक् श्रवण एवं दृष्टि आदि शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के गुण हैं। शारीरिक अवयवों की हैसियत तो मात्र यंत्रों की है जो विशेष प्रकार के कार्यों का सम्पादन करते हैं। इन यन्त्रों के अभाव में भी अन्य रूप में आत्मा के लिए देखना और बोलना और समझना सबकुछ सम्भव रहता है। इसके लिए वह शारीरिक अवयवों— कान, आँख, मस्तिष्क और जिह्वा पर आश्रित नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि शारीरिक यन्त्रों के बिना इन गुणों की कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर के बारे में हम सबकी धारणा है कि वह शारीरिक यन्त्रों के बिना इन गुणों से विभूषित है।
(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब कोई बन्दा झूठ बोलता है तो फ़रिश्ता उसके वचन की दुर्गन्ध से एक मील दूर चला जाता है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : भौतिक वस्तुओं की सुगन्ध और दुर्गन्ध की भाँति मानवीय कर्मों और वचनों की भी अपनी सुगन्ध और दुर्गन्ध होती है। भौतिकवाद के वर्चस्व के कारण हम सड़ी-गली चीज़ों की दुर्गन्ध तो महसूस करते हैं लेकिन उन चीज़ों की दुर्गन्ध महसूस नहीं करते जिनकी दुर्गन्ध उस दुर्गन्ध की तुलना में सहस्त्रों गुना अधिक होती है।
इसी प्रकार फूलों की सुगन्ध का तो पता हमें चल जाता है लेकिन उस सुगन्ध और स्वाद को हम महसूस करने में अक्षम रहते हैं जिसकी तुलना में आम सुगन्ध और स्वाद हेय हैं। सामान्य रंग और गन्ध अपने सौन्दर्य के कारण हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं किन्तु दुख तो यह है कि सत्य एवं आत्मिक सौन्दर्य से अपरिचित ही हम दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं।
फ़रिश्तों की चेतना अत्यन्त सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। इसलिए वे हमारे अच्छे-बुरे कर्मों की सुगन्ध या दुर्गन्ध को महसूस करते हैं और झूठ की दुर्गन्ध के कारण दूर हट जाते हैं। ईश्वर के ये प्रतिष्ठित सृष्टजीव हमारे झूठ की दुर्गन्ध के कारण हमसे दूर भागें यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, लेकिन हमें इसकी ख़बर भी नहीं होती कि ईश्वर के फ़रिश्ते जो ईश्वर के अत्यन्त निकटवर्ती और प्रकाशतुल्य सृष्टजीव हैं उन्हें हमारी बुराइयों से तकलीफ़ होती है और वे हमसे निकट होने के बजाय हमसे दूर भागते हैं। यहाँ यह बात दृष्टि में रहे कि केवल झूठ ही से नहीं बल्कि परनिन्दा और बदज़बानी आदि की दुर्गन्ध से भी ये पवित्र जीव हमसे दूर भागते हैं।
फ़रिश्तों के अतिरिक्त इनसानों में भी जिस व्यक्ति की आध्यात्मिकता उसकी भौतिकता पर वर्चस्व रखती है उसे भी कर्मों के सुगन्ध या दुर्गन्ध का बोध हो सकता है।
मानव, शरीर ही नहीं आत्मा भी रखता है बल्कि मूलतः वह आत्मा ही है जो भौतिकता से सर्वथा मुक्त है। ईश्वर स्वयं भौतिकता से परे है और दिक्काल की सीमाओं से मुक्त है। इसलिए भौतिकता ही को सब कुछ समझ लेना दृष्टिहीनता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस प्रकार लाभ और हानि, सुख और दुख, प्रियता और अप्रियता, प्रकाश और अन्धकार, उच्चता और अधमता, प्रशंसनीय और अप्रशंसनीय, सुन्दरता और असुन्दरता का अनुभव हमें इस भौतिक जगत् में होता है, ठीक इसी प्रकार बल्कि इससे भी बढ़कर इन चीज़ों का एहसास हमें आध्यात्मिक जगत् में होता है। जो सौन्दर्य और गुण हमें भौतिक चीज़ों में दृष्टिगोचर होते हैं उनका उस सौन्दर्य और ख़ूबसूरती से कोई मुक़ाबला नहीं जो उन चीज़ों में पाई जाती है जो भौतिकता से मुक्त हैं। सड़ी हुई चीज़ों की दुर्गन्ध से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह दुर्गन्ध उस दुर्गन्ध की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उस चीज़ से आत्मा को पहुँचती है जो आत्मा के लिए सर्वथा सड़ाँध है।
हम खाने-पीने का स्वाद और फूलों की सुगन्ध को तो महसूस कर लेते हैं लेकिन उस स्वाद और सुगन्ध को महसूस करने में साधारणतः असमर्थ रहते हैं जो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। आवश्यकता है कि हम भौतिक आस्वादों से अधिक ईमानी, आध्यात्मिक एवं वास्तविक नेमतों और आस्वादों से परिचित हों और दुनिया और आख़िरत में स्वयं को दुखद अभावों से बचा सकें।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी के झूठ के लिए यही पर्याप्त है कि वह जो कुछ सुने उसे बयान करता फिरे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : प्रत्येक सुनी-सुनाई बात बिना पुष्टि के बयान करते फिरना भी एक प्रकार से झूठ में लिप्त होना है। इस प्रकार की बातों में इसकी अधिक सम्भावना होती है कि बात निराधार और ग़लत हो। आदमी को चाहिए कि वह जो कुछ भी कहे पहले उसके बारे में आश्वस्त हो ले। अफ़वाहों को हवा देना किसी भी प्रकार सही नहीं हो सकता। इससे विभिन्न फ़ितनों को सिर उठाने का मौक़ा मिलता है जिसका अनुभव आए दिन लोगों को होता रहता है।
(4) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मुझे तुमसे ज़्यादा हदीसें वर्णन करने से यह चीज़ रोकती है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“जो व्यक्ति जान-बूझकर मुझसे झूठी बात सम्बद्ध करे वह अपना ठिकाना नरक में बना ले।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : ग़लत तौर पर कोई बात किसी से सम्बद्ध करके बयान करना यूँ भी हराम है लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सम्बद्ध करके कोई ऐसी बात कहनी जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने न कही हो, अत्यन्त गम्भीर क़िस्म का अपराध है जो अक्षम्य है। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसे व्यक्ति को नरक की चेतावनी दी है। गढ़ी हुई और ग़लत क़िस्म की हदीसों से धार्मिक व्यवस्था और उसकी प्रकृति के बिगड़ने की बड़ी आशंका होती है। इसलिए इस अपराध के गम्भीर होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।
यह हदीस अत्यन्त प्रामाणिक है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन के कारण संयमी लोग हमेशा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सम्बद्ध करके कोई हदीस बयान करने में सदैव सतर्क रहे हैं। कितने दुख का विषय है कि इस चेतावनी और डरावे के बावजूद कितनी ही कमज़ोर और मनघड़त हदीसें भी मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हो गई हैं। और आज भी धर्मोपदेशक और लेखक इस सम्बन्ध में जिस असावधानी का परिचय देते आ रहे हैं वह विद्वानों की दृष्टि से ओझल नहीं।
(5) हज़रत ख़ुरैम-बिन-फ़ातिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई। फिर जब लोगों की ओर मुड़े तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सीधे खड़े हो गए और कहा—
"झूठी गवाही देना ईश्वर का साझीदार बनाने के तुल्य है।" यह बात आपने तीन बार कही। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की आयत पढ़ी— “अतः तुम मूर्तियों की गंदगी से बचो, और बचो झूठी बात से, इस प्रकार कि अल्लाह ही की ओर होकर रहो, उसका साझीदार न ठहराओ।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जिन आयतों का हवाला दिया है वे सूरा अल-हज्ज की आयतें (31-32) हैं। इन आयतों में काले नूर (झूठ) का बहुदेववाद और मूर्तिपूजा के साथ उल्लेख किया गया है। और एक ही शब्द के द्वारा दोनों से बचने का आदेश दिया गया है। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह निष्कर्ष निकाला कि झूठी गवाही और बहुदेववाद सहजातीयता की दृष्टि से एक ही कोटि की चीज़ें हैं। झूठी गवाही का सम्बन्ध एकेश्वरवाद से नहीं, बल्कि बहुदेववाद ही से हो सकता है। एकेश्वरवाद सत्य और बहुदेववाद सर्वथा झूठ और मिथ्यारोपण है। मुसलमान जिस प्रकार बहुदेववाद और मूर्तिपूजा से घृणा करते हैं उसी प्रकार उन्हें झूठी गवाही देने से घृणा होनी चाहिए। ताकीद के लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी बात को तीन बार दोहराया।
(6) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया। उस समय अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे घर में बैठे हुए थे। मेरी माँ ने कहा कि दौड़कर आओ, मैं तुम्हें कुछ दूँगी। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मेरी माँ से कहा—
“तुम उसे क्या देना चाहती हो?” उन्होंने कहा कि मेरी उसे एक खजूर देने की इच्छा है। इसपर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा, "याद रखो, अगर तुम उसे कुछ न देतीं तो एक झूठ तुम्हारे कर्मपत्र में लिख दिया जाता।” (हदीस : अबू-दाऊद, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान)
व्याख्या : आम तौर पर लोग बच्चों को बहलाने, उन्हें डराने या उनसे कोई काम लेने के लिए कोई झूठी बात कहने में कोई बुराई नहीं समझते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ख़याल हुआ कि कहीं आम रिवाज के मुताबिक़ अब्दुल्लाह-बिन-आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) (जो उस समय बच्चे थे) की माँ ने भी झूठा वादा करके उन्हें अपने पास बुलाना न चाहा हो। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा कि तुम उसे क्या देना चाहती हो।
इस हदीस का सार यह है कि आदमी को किसी हाल में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि उसकी गणना झूठों में न हो। यहाँ यह बात भी दृष्टि में रहे कि माँ-बाप अगर बच्चों से झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलने लगेंगे और उनको इसमें कोई बुराई महसूस न होगी।
(7) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन में प्रत्येक स्वभाव का पाया जाना सम्भव है सिवाय विश्वासघात और झूठ के।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
मोमिन के स्वभाव और प्रकृति में इसकी गुंजाइश नहीं कि वह विश्वासघाती और झूठा हो। मोमिन अगर सही अर्थों में मोमिन है तो उससे झूठ और विश्वासघात की आशा नहीं की जा सकती। रही दूसरी कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ तो उनकी सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन झूठ और विश्वासघात जैसे कपटपूर्ण दुर्गुणों का ईमान से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अगर किसी मुसलमान में झूठ और विश्वासघात का ऐब मौजूद है तो उसे अपने ईमान की ख़ैर मनानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसका जीवन इन बुराइयों से मुक्त हो क्योंकि इसके बिना वास्तविक ईमान नसीब नहीं हुआ करता।
(8) बह्ज़-बिन-हकीम अपने पिता के माध्यम से अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अफ़सोस उस व्यक्ति पर जो अपनी बातचीत में लोगों को हँसाने के उद्देश्य से झूठ बोले! उसपर अफ़सोस! उसपर अफ़सोस!" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद, दारमी)
व्याख्या : हँसने-हँसाने और विनोदपूर्ण संगति के आनन्द में वृद्धि के लिए झूठ का सहारा लेना सर्वथा अनुचित है चाहे इससे किसी को कष्ट पहुँचने की आशंका न भी हो। ज़ुबान को हर हाल में हमेशा पवित्र रखना चाहिए। उसे झूठ से अपवित्र करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसके अतिरिक्त एक कमज़ोरी से दूसरी कमज़ोरियों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इससे समाज में झूठ के प्रचलन की आशंका उत्पन्न होती है और मोमिन को झूठ बोलने और झूठी बातों से जो घृणा होनी चाहिए उसमें कमी हो जाती है।
(9) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल) ने कहा—
"सबसे बड़ा झूठा आरोप यह है कि आदमी अपनी आँखों को वह स्वप्न दिखाए जो उन आँखों ने देखा नहीं।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात अगर कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा स्वप्न गढ़कर लोगों से कहता है तो यह झूठ ही नहीं एक मिथ्या आरोप भी है, और बड़ा आरोप। क्योंकि ये आरोप नुबूवत के झूठे दावे के सदृश है। स्वप्न में आदमी जो कुछ भी देखता है उसमें उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। ईश्वर की ओर से स्वप्न के द्वारा बन्दे को भविष्य में घटनेवाली किसी घटना की सूचना भी दी जा सकती है और स्वप्न किसी बात के सम्बन्ध में एक चेतावनी या शुभ सूचना भी हो सकता है। इसी लिए सच्चे स्वप्न को नुबूवत का चालीसवाँ भाग कहा गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मनगघड़त स्वप्न बयान करता है तो मानो वह ईश्वर की ओर से ऐसी बात कह रहा होता है जिसका ईश्वर से सिरे से कोई सम्बन्ध ही नहीं होता।
(10) हज़रत उम्मे-कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"वह व्यक्ति झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के उद्देश्य से कोई भलाई की बात कह दे। और किसी को किसी की ओर से भली बात पहुँचा दे।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : कभी-कभी दो व्यक्तियों या दो पक्षों के बीच कुछ ऐसे झगड़े खड़े हो जाते हैं जिनके परिणाम अत्यन्त हृदयविदारक सिद्ध होते हैं। वैरभाव और शत्रुता के कारण प्रत्येक पक्ष ऐसी कार्रवाई करने लग जाता है जिससे ख़ून-ख़राबे तक की नौबत आ जाती है। ऐसी सूरत में अगर कोई निःस्वार्थ भाव से उनके बीच सुलह कराने का प्रयास करता है और इस सम्बन्ध में वह इसकी आवश्यकता महसूस करता है कि यह एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को ऐसी प्रसन्न करनेवाली बातें पहुँचाए जिससे दोनों के बीच विश्वास का वातावरण बने और शत्रुता की भड़कती हुई ज्वाला शान्त हो तो ऐसी प्रसन्न करनेवाली बातों के पहुँचाने में कोई हर्ज नहीं है। बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी द्विअर्थी बातों के कहने की पूरी गुंजाइश है जिससे किसी शुभ की आशा की जा सकती हो। इसे 'तौरिया' कहते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में इसमें कुछ अधिक ही गुंजाइश है। उनके मतानुसार आवश्यक और उचित उद्देश्यों के तहत अगर झूठ बोलना अपरिहार्य हो जाए तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि कभी-कभी तो झूठ से काम लेना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति किसी अत्याचारी से, जो उसकी हत्या करना चाहता है, बचकर हमारे घर में छिपा हुआ है तो अनिवार्य है कि हम उसे बचाने के लिए उस अत्याचारी व्यक्ति के पूछने पर साफ़ कह दें कि वह यहाँ नहीं है लेकिन यह उसी समय जबकि तौरिया से काम न चल सके। वरना जहाँ तक सम्भव हो तौरिया से काम लें। निरे और स्पष्ट झूठ से बचें। तौरिया का एक उदाहण आगे की हदीस में आ रहा है। इब्ने-क़ुतैबा ने इसकी कई मिसालें दी हैं।
(देखें तावीले-मुख़्तलिफ़ुल अहादीस, पृ. 15 से 48)
(11) हज़रत सुवैद-बिन-हनज़ला (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित होने के इरादे से निकले। हमारे साथ वायल बिन-हुज्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी थे। उन्हें रास्ते में उनके एक दुश्मन ने पकड़ लिया। लोगों को क़सम खाने में संकोच हुआ। मगर मैंने क़सम खा ली कि वह मेरा भाई है। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। फिर जब हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए तो मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इसकी सूचना दी कि इन लोगों को तो क़सम खाने में संकोच हुआ मगर मैंने क़सम खा ली कि वह मेरा भाई है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुमने सच कहा, मुसलमान मुसलमान का भाई ही होता है। न वह उसके अधिकारों का हनन करता है, न समय पर उसकी सहायता करने से भागता है और न उसे (किसी संकट आदि में) ग्रस्त कर सकता है।" (हदीस : अबू दाऊद)
पथभ्रष्टता
(1) हज़रत सफ़िय्या (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शैतान इनसान (की नाड़ियों) में इस प्रकार दौड़ता है जैसे रक्त-संचार।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह एक महत्वपूर्ण हदीस का एक टुकड़ा है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक रात अपनी पत्नी हज़रत सफ़िय्या (रज़ियल्लाहु अन्हा) के साथ जा रहे थे कि रास्ते में अनसार के दो व्यक्ति मिले। उन्होंने आपको देखा तो तेज़-तेज़ चलने लगे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि अपनी चाल चलो (तेज़ न चलो)। ये सफ़िय्या-बिन्त-हुयय्य हैं (जो मेरी पत्नी हैं। कोई अन्य स्त्री मेरे साथ नहीं है)। उन्होंने कहा कि सुबहानल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल! (अर्थात, ख़ुदा न करे! क्या आप के बारे में हमें कोई बदगुमानी हो सकती है?) इसपर आपने कहा कि शैतान आदमी की नाड़ियों में रक्त की भाँति फिरता है। मतलब यह है कि मुझे शंका हुई कि कहीं शैतान को यह अवसर न मिल जाए कि वह तुम्हारे दिलों में कोई बुरा विचार डाल दे।
ज्ञात हुआ कि शैतान का प्रयास ही यह होता है कि वह इनसान को गुनाह और बुराई में ग्रस्त कर दे। वह अपने काम में पूरी तरह लगा हुआ है। रक्त की गर्दिश इनसान को जीवित रखती है। शैतान अगर अपने उपाय में सफल होकर मानव के विचार और मन और उसकी प्रवृत्तियों तक को प्रभावित कर सकता है तो इस प्रकार मानव का मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। एक हदीस में आया है कि मेरी उम्मत (समुदाय) में ऐसे लोग पैदा होंगे जिनमें गुमराहियाँ इस प्रकार समा जाएँगी जैसे 'कलब' (हाईड्रोफ़ोबिया) का रोग इनसान की नस-नस और जोड़-जोड़ में समा जाता है। कलब एक बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने से होती है।
गुनाह
(1) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! कौन-सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह कि तुम किसी को ईश्वर का प्रतिद्वन्द्वी बनाओ हालाँकि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है।" पूछा, "फिर कौन-सा?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह कि तुम अपनी सन्तान की हत्या इस डर से करो कि वह खाने में तुम्हारी शरीक होगी।" पूछा, “फिर कौन-सा?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "यह कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से व्यभिचार करो।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इन कबीरा (बड़े) गुनाहों का क़ुरआन में भी एक साथ उल्लेख हुआ है—
“जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इष्ट-पूज्य को नहीं पुकारते और न नाहक़ किसी जीव को (जिसके क़त्ल को अल्लाह ने हराम किया है) क़त्ल करते हैं— यह और बात है कि हक़ की माँग यही हो— और न वे व्यभिचार करते हैं। जो कोई यह काम करे वह गुनाह के वबाल से दोचार होगा।" (25:68)
गुनाह आदमी की दुष्ट प्रवृत्ति का प्रमाण होता है और बड़े गुनाह जिन्हें 'कबाइर' कहते हैं उनमें ग्रसित रहनेवाले तो ईश्वर के घोर अवज्ञाकारी और सत्य और न्याय के दुश्मन होते हैं। उनपर ईश्वर का क्रोध भड़कता है और अन्ततः ऐसे लोगों को ऐसे सन्ताप और ऐसी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा जिसका सही अनुमान करना भी आज असम्भव है। इस्लाम की शिक्षा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि इनसान ईश्वर के क्रोध और प्रकोप से बचे और जीवन में कोई ऐसी नीति न अपनाए जो उसके लिए घाटे और हलाकत का कारण बने। वह एक ओर इनसान को दूसरों के अधिकारों से परिचित कराता है और दूसरी ओर उसे उसके अपने दायित्वों से अवगत कराता है।
(2) इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) वर्णन करते हैं कि उन्हें यह हदीस पहुँची कि हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने, जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की धर्मपत्नी थीं, कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उस समय भी तबाह होंगे जबकि हमारे बीच नेक लोग मौजूद होंगे? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हाँ, उस समय जबकि गुनाहों की अधिकता हो जाए।" (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : अर्थात जब गन्दगी और बुराई अत्यधिक बढ़ जाए तो इसकी बड़ी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि ईश्वर क़ौम को हलाक कर दे। ऐसी स्थिति में नेक लोग भी हलाक हो सकते हैं। यह अलग बात है कि आख़िरत में उनका हश्र अवज्ञाकारियों और ईश-द्रोहियों के साथ न हो लेकिन दुनिया में जब सार्वजनिक तबाही आती है तो क़ौम के नेक लोगों का उससे बच सकना मुश्किल होता है। और अगर नेक और भले लोग क़ौम को बुराई और उसके अंजाम से डराने और उसको सीधे रास्ते पर लाने के प्रयास से बेपरवाही करते रहे हों तो फिर वे अपनी इस कोताही के दण्ड से कैसे बच सकेंगे।
(2)
कुरुचि
अहंकार
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल) ने कहा—
“जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।” एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अल्लाह सौन्दर्यवान है और सौन्दर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से अनुमान किया जा सकता है कि स्वर्ग कितना स्वच्छ और पवित्र स्थान है। जन्नत में किसी प्रकार की गन्दगी और अशुद्धता नहीं पाई जा सकती चाहे वह गन्दगी देखने में कितनी ही छोटी क्यों न हो। अहंकार भी एक नैतिक अशुद्धता और गन्दगी है। इस गन्दगी को लिए हुए कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता। जन्नत के वासी वही लोग होंगे जिनमें तनिक भी गन्दगी न हो।
अगर कोई व्यक्ति जाइज़ सीमा के अन्दर वस्त्र और आवास में सुरुचि और सौन्दर्य का ध्यान रखता है तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे। ईश्वर स्वयं सौन्दर्यवान है और सौन्दर्य को पसन्द करता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी और जिस रूप में भी सौन्दर्य पाया जाता है वह वास्तव में ईश्वर ही के सौन्दर्य का द्योतक है। यहाँ यह बात सामने रहे कि जीवन में सौन्दर्य आन्तरिक और बाह्य दोनों ही पहलुओं से अपेक्षित है। हमारे ज़ाहिरी रहन-सहन, रख-रखाव और वस्त्र आदि में भी किसी कुरूपता और बेढंगेपन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और हमारे विचारों और कर्मों के द्वारा भी सौन्दर्य ही की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जिस चीज़ को साधारण बोलचाल में हम धर्म कहते हैं, गहराई में जाने के बाद वही चीज़ सौन्दर्यानुभव और सौन्दर्यबोध बन जाती है।
यह हदीस बताती है कि तथ्यात्मक दृष्टि से अहंकार यह है कि आदमी को सत्य की चिन्ता न हो और वह लोगों को हेय दृष्टि से देखता हो। यह चीज़ उसके अन्तर्मन की दुष्टता का स्पष्ट प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी नीति अपनाता है जिसमें ईश्वर के अधिकारों और हक़ और सच का ध्यान नहीं रखा गया है या उसके रहन-सहन के अन्दाज़, उसके स्वयं को सजाने-संवारने के पीछे यह भावना कार्यरत रहती है कि दूसरे उसे बड़ा समझें और उसके आगे अपने को तुच्छ समझें तो यह नीति स्पष्टतः अहंकारपूर्ण नीति है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अपनी इस नीति के साथ वह कभी भी उस वास्तविक महानता को प्राप्त नहीं कर सकता जो उम्र भर उसकी प्रतीक्षा में रहती है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन आदमी ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन ईश्वर उनसे बात न करेगा और न उन्हें उत्कृष्टता प्रदान करेगा।" और एक हदीस में यह भी है कि "वह उनपर दृष्टिपात भी नहीं करेगा।" "और इनके लिए दुखदायी यातना है। एक बूढ़ा व्यभिचारी, दूसरा झूठा शासक, तीसरा दरिद्र और निर्धन अहंकारी।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थ यह है कि ईश्वर ऐसे लोगों से इतना क्रुद्ध और अप्रसन्न होगा कि वह उन्हें इस योग्य ही न समझेगा कि उन्हें अपने से बात करने का सौभाग्य प्रदान करे या कृपापूर्वक उन्हें देखे या उन्हें उत्कृष्टता प्रदान करे और उन्हें प्रशंसित घोषित करे।
व्यभिचार प्रत्येक हालत में एक दुष्कर्म है लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में जबकि कामेच्छा अधिकांशतः ठंडी पड़ चुकी होती है, अगर कोई व्यभिचार का अपराधी बनता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसके स्वभाव में अत्यन्त दुष्टता पाई जाती है। इसी प्रकार झूठ बोलना हरेक के लिए बुरा है लेकिन एक शासक के लिए तो यह मृत्यु से कम नहीं। इसलिए कि आदमी झूठ कभी लाभ उठाने के लिए बोलता है और कभी हानि से बचने के लिए, मगर एक शासक को इसकी क्या आवश्यकता है कि वह झूठ का सहारा ले। एक शासक का दायित्व तो यह है कि वह राज्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखे और जनसाधारण की समस्याओं को सुलझाने की चिन्ता करे और इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएँ पहुँच सकें और वह सुखपूर्वक रह सके। अब अगर शासक इतना गिरा हुआ है कि झूठ बोलने में भी उसे संकोच नहीं तो अपने शासनक्षेत्र में सत्कर्मों के प्रसार में वह आख़िर किस प्रकार सफल हो सकता है।
इसी प्रकार अहंकार और घमंड यूँ तो किसी के लिए उचित नहीं है लेकिन एक ग़रीब और दरिद्र व्यक्ति अगर अहंकार में पड़ा हो तो यह अत्यन्त अधमता और नीचता की बात होगी। इसलिए कि उसके यहाँ सिरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जो अहंकार का आधार बन सके। फिर भी यदि वह अहंकार में पड़ा है तो इसे उसकी मानसिक गिरावट और दुष्टता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि प्रतापवान ईश्वर कहता है—
“बड़ाई मेरी चादर और महानता मेरा तहमद है। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक को भी मुझसे छीनना चाहे तो मैं उसे नरक की आग में डाल दूँगा।” और एक रिवायत में है कि, “मैं उसे नरकाग्नि में फेंक दूँगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में मिसाल के द्वारा एक बड़े तथ्य को मन में बिठाने का प्रयास किया गया है। अभिप्राय यह है कि बड़ाई और महानता ईश्वर के ऐसे गुण हैं जो उसी के लिए विशिष्ट हैं। बन्दों को जो चीज़ शोभा देती है वह बड़ाई और महानता नहीं बल्कि वह विनम्रता और विनयशीलता है।
जो व्यक्ति घमण्ड करे और बड़ा बनना चाहे और महानता और बड़ाई का दावेदार हो वह ईश्वरीय चादर या तहमद छीनना चाहता है।
(4) हज़रत हारिसा-बिन-वह्ब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“क्या मैं तुम्हें ख़बर दूँ कि नरकवासी कौन हैं? प्रत्येक उद्दंड, कठोर और अहंकारी।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात उद्दंडता, कठोरता और अहंकार ये ऐसे अवगुण हैं जिनके कारण आदमी की गणना नरकवालों में होती है। अब अगर वह अपने सुधार की ओर ध्यान नहीं देता तो ईश्वर के प्रकोप से उसे बचानेवाली कोई चीज़ न होगी। क़ुरआन में भी विभिन्न स्थानों पर इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अहंकारियों का ठिकाना नरक ही होगा। उदाहरणस्वरूप क़ुरआन में कहा गया है—
“प्रवेश करो नरक के द्वारों में, उसमें सदैव रहने के लिए। अतः बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का!" (40:76)
क़ौमों के कुफ़्र और इनकार के पीछे बहुधा उद्दंडता और अहंकार की भावना ही कार्यरत रही है। अहंकार के कारण कितनी ही क़ौमें ईमान की निधि से सर्वथा वंचित रहीं। उन्होंने अपने रसूलों का इनकार किया। दुनिया में भी वे ईश्वर के कोप का भाजन बनीं और आख़िरत में जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगी।
(5) हज़रत मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति इससे प्रसन्न हो और यह पसन्द करे कि लोग उसके सामने खड़े रहें तो उसे चाहिए कि वह नरक में अपने आसन की जगह तैयार करे।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह आदेश सूचना के अर्थों में है। अर्थात उसके लिए नरक में प्रवेश करना अनिवार्य है। इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति अहंकार के कारण इस बात का इच्छुक रहता है कि लोग उसके सम्मान में झुकें और उसके आगे हाथ बाँधकर खड़े हों, उसे समझ लेना चाहिए कि ईश्वर के यहाँ उसका स्थान स्वर्ग नहीं, नरक है। नरक की भड़कती हुई ज्वाला उसे बता देगी कि वह प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित।
ख़ुदपसन्दी और महत्वाकांक्षा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन चीज़ें मुक्त करनेवाली और तीन विनष्ट करनेवाली हैं। मुक्त करनेवाली चीज़ें ये हैं— छिपे और खुले अल्लाह का डर रखना। प्रसन्नता की अवस्था हो या क्रोध की, हर हाल में सत्य कहना। और निर्धनता हो या सम्पन्नता, प्रत्येक स्थिति में मध्यमार्ग अपनाना। रहीं विनष्ट कर देनेवाली चीज़ें तो वे ये हैं— मनेच्छा, आदमी जिसका अनुपालन करे, वह लोभ और कृपणता जिसका कि वह अधीनस्थ बनकर रहे और आदमी की ख़ुदपसन्दी। और यह (अन्तिम) इन सबमें सर्वाधिक गम्भीर है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : विचार करने से मालूम होता है कि ये तीन चीज़ें —अर्थात यह कि आदमी हर हाल में अल्लाह से डरे, सत्य कहे और मध्यमार्ग पर रहे— अत्यन्त महत्वपूर्ण और मौलिक हैं। इन्हें अपनाने के बाद आदमी न केवल यह कि आख़िरत में हलाकत और तबाही से बचेगा बल्कि दुनिया में भी वह नाना प्रकार की विपत्तियों और उपद्रवों से सुरक्षित रहकर अधिक से अधिक समय सत्य की सेवा के लिए निकाल सकेगा।
अनेक व्यक्तित्वों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब भी किसी व्यक्ति ने जीवन की बाग-डोर मन की इच्छाओं को सौंप दी और संकीर्ण-हृदयता और लोभ और कृपणता उसका स्वभाव बन गया, उसके नैतिक जीवन का अन्त होकर रहा। 'हुदा' (ईश्वरीय मार्गदर्शन) के विपरीत जिस किसी ने भी 'हवा' (मनेच्छा) को प्राथमिकता दी और विशाल-हृदयता और उदारता के विपरीत संकीर्णता और लोभ-लिप्सा और कृपणता को अपना स्वभाव बनाया, वह न संसार में कोई प्रतिष्ठा अर्जित कर सका और न आख़िरत में उसका कोई सम्मान होगा। ऐसे व्यक्ति का कदापि कोई उच्च और महान जीवनोद्देश्य नहीं हो सकता। और न ही उससे मानवता की किसी बड़ी सेवा की आशा की जा सकती है। कल्याण और सफलता के लिए आवश्यक है कि आदमी का हृदय विशाल और दृष्टि उच्च हो। क़ुरआन में है— “और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिया जाए ऐसे ही लोग सफल हैं।" (59:9, 64:16)
ख़ुदपसन्दी और महत्वाकांक्षा को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सबसे बढ़कर गम्भीर और घातक ठहरा रहे हैं। एक तो आत्मश्लाघा स्वयं एक अत्यन्त घिनावनी चीज़ है। दूसरे यह कि जिस व्यक्ति को यह रोग लग जाता है उसके सुधार की आशा अत्यन्त कम रह जाती है। ख़ुदपसन्दी एक ऐसा भ्रमजाल है जिससे निकल पाना अत्यन्त कठिन होता है। ख़ुदपसन्दी के लिए मार्गदर्शन की सम्भावनाएँ साधारणतः शेष नहीं रहतीं। वह अपनी ग़लतियों को नहीं जान सकता। न उसके अन्दर कुछ जानने और समझने की इच्छा और तड़प ही शेष रहती है। हृष्ट-पुष्ट और सबल शरीर का दम्भ हो या अपनी धार्मिकता का भ्रम, वह उन ही पर गौरवान्वित होता है। यही अहंकार और आत्मग्रस्तता उसके जीने का मानसिक सहारा बन जाती है। ऐसी स्थिति में उसके सुधार का काम कितना दुष्कर होता है इसका अनुमान प्रत्येक दृष्टिवान कर सकता है।
(2) हज़रत मिक़दाद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुम गुणगान करनेवालों को देखो तो उनके मुँह पर ख़ाक डाल दो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात उनके गुणगाान से प्रसन्न मत हो बल्कि उसे अप्रिय समझो। अगर वे तुम्हारे गुणगान के द्वारा अपने किसी भौतिक लाभ के लिए तुमसे कोई ग़लत काम कराना चाहते हों तो इसमें उन्हें कदापि सफल होने न दो।
(3) हज़रत अबू-बकर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुममें से कोई यह न कहे कि मैंने रमज़ान भर पूरे रोज़े रखे और पूरे मास क़ियाम (रात्रि उपासना) में खड़ा रहा।" (हदीस : अबू दाऊद)
व्याख्या : इससे स्पष्टतः ज्ञात होता है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आदमी अपने गुणों का बखान करता फिरे और इसमें अतिशयोक्ति से काम ले। ऐसा व्यक्ति अगर महत्वाकांक्षा के रोग में ग्रस्त न भी हो तब भी इसकी सम्भावना बनी रहती है कि वह इस घातक रोग में ग्रस्त हो जाए।
ख्याति-मोह
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने दुनिया में ख्याति-वस्त्र धारण किया ईश्वर उसे क़ियामत के दिन हीनत्व का वस्त्र पहनाएगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)
व्याख्या : अबू-दाऊद में हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से एक हदीस उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने प्रसिद्ध होने के उद्देश्य से कपड़ा पहना, क़ियामत के दिन अल्लाह उसे वैसा ही कपड़ा पहनाएगा।" (अबू-अवाना की हदीस में इतना और भी है कि) "फिर उसमें आग लगा देगा।"
कपड़ा हो या जूता आदि या कोई भी चीज़, आदमी उसे आवश्यकता समझकर प्रयोग करे न कि लोगों पर अपनी बड़ाई प्रदर्शित करने के लिए वह उसे प्रयोग करे और उसे अपनी बड़ाई के प्रदर्शन का साधन बनाए। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कपड़ा इस उद्देश्य से पहनता है कि लोगों में उसका नाम हो और लोगों के दिलों पर उसकी महानता और उसके व्यक्तित्व का सिक्का जम सके, इसी प्रकार अगर कोई अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक शुद्धता को व्यक्त करने के लिए संन्यासियों और भिक्षुओं का विशेष वस्त्र धारण किए रहता है तो ईश्वर को यह अन्दाज़ कदापि प्रिय नहीं है क्योंकि यह ख़ुदपसन्दी और अहंकार का परिचायक है। ऐसे लोग क़ियामत के दिन अपमानित होकर रहेंगे।
यहाँ यह तथ्य भी दृष्टि में रहे कि इस्लामी सभ्यता में न धनी लोगों के लिए कोई विशिष्ट लिबास निर्धारित किया गया है और न किसी ऐसे धार्मिक वर्ग को सहन किया गया है जो अपने आप को सबसे उच्च, श्रेष्ठ और विशिष्ट समझता हो और अपनी धार्मिक पवित्रता के प्रचार में लगा हो।
(2) हज़रत तरीफ़-अबू-तमीमा से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैं सफ़वान (रज़ियल्लाहु अन्हु) और जुंदुब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके साथियों के पास मौजूद था। वे लोगों को नसीहत कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या आप ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कुछ सुना है? उन्होंने कहा कि मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि, "जिस किसी ने लोगों को सुनाने के उद्देश्य से और ख्याति के लोभ में कुछ किया तो ईश्वर क़ियामत के दिन उसके छिपे हुए ऐब प्रकट कर देगा। और जिस किसी ने किसी को कठिनाई में डाला तो अल्लाह क़ियामत के दिन उसपर मुशक़्क़त का बोझ डाल देगा।" लोगों ने कहा कि हमें और भी नसीहत करें तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "सबसे पहले इनसान का पेट सड़ता है। इसलिए जिस किसी व्यक्ति को यह सामर्थ्य प्राप्त हो कि वह विशुद्ध और स्वच्छ चीज़ ही खाए तो उसे चाहिए कि वह ऐसा करे। और जो व्यक्ति यह कर सकता हो कि उसके और स्वर्ग के बीच उसका बहाया चुल्लू भर ख़ून भी आड़े न आए तो उसे चाहिए कि वह ऐसा अवश्य करे।" मैंने अबू-अब्दुल्लाह से कहा कि कौन कहता है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सुना है? क्या जुंदुब ने कहा है? उन्होंने कहा कि "हाँ, जुंदुब ने कहा है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : जो कोई अपनी ख्याति का भूखा है तो उसे जान लेना चाहिए कि प्रतिष्ठा और ख्याति उसे मिलती है जिसे ईश्वर प्रदान करे। प्रतिष्ठा वास्तव में ईश्वर की महानता के आगे अपने आप को झुका देने ही में है। जो व्यक्ति इसे किसी और तरीक़े से प्राप्त करने का प्रयास करे वह स्वयं को अपमानित करके रहेगा। इसलिए कि दुनिया में उसने ईश्वर के प्रताप और महानता का कुछ भी आदर न किया। अगर सही अर्थों में दुनिया के जीवन में उसे ईश्वर की महानता और बड़ाई का एहसास होता तो उसे सिरे से अपनी प्रसिद्धि का विचार भी न आता।
ईश्वर को अपने बन्दों से प्यार है। अब अगर कोई ईश्वर के बन्दों में से किसी को कष्ट पहुँचाता है और उसे किसी कठिनाई और विपत्ति में डाल देता है तो ईश्वर उसे क़ियामत के दिन कठिनाई में डालकर रहेगा। तात्पर्य यह कि दुनिया में इनसान का अपना चरित्र जैसा होगा उसी के अनुसार आख़िरत के जीवन में उसे दंड या पुरस्कार प्राप्त होगा। इस उसूल की रौशनी में हरेक व्यक्ति सरलतापूर्वक यह अनुमान कर सकता है कि वह अपने लिए किस प्रकार की आख़िरत चाहता है।
ग़ाफ़िल और सत्य से अपरिचित व्यक्ति को सबसे बढ़कर चिन्ता अपना पेट भरने की होती है, जबकि आदमी के मरने के बाद सभी अंगों में सबसे पहले उसका पेट ही सड़ता है। ये खाने-पीने की लज़्ज़तें क्षणिक हैं। इनसान क्षणिक आनन्द की प्राप्ति के लिए कदापि पैदा नहीं किया गया। उसकी प्रकृति तो उस चीज़ की खोज में रहती है जो क्षणिक न हो बल्कि शाश्वत हो। और सदा शेष रहनेवाली नेमतों का अधिकारी इनसान तभी हो सकता है जबकि वह संवेदनशील, सुचरित्र और परहेज़गार हो। इसी लिए कहा गया कि इनसान को चाहिए कि वह स्वच्छ और विशुद्ध भोजन ही से अपना पेट भरे। और वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान है जिसको यह अवसर प्राप्त हो कि वह अपना पेट हलाल और शुद्ध आहार और केवल हलाल और शुद्ध आहार से भरे।
अत्याचारी का अत्याचार उसे जन्नत में प्रवेश करने से रोक देगा। समस्त अत्याचारों में हत्या या रक्तपात इतना बड़ा अत्याचार है जिसके अत्याचार होने से किसी को इनकार नहीं हो सकता। हत्या और रक्तपात की जघन्यता ही है जिसके कारण क़ियामत में सबसे पहले लोगों के बीच हत्या के मामलों के फ़ैसले सुनाए जाएंगे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
अब जो व्यक्ति भी स्वर्ग, जो ईश्वरीय प्रसन्नता और उसकी रहमत का सबसे बड़ा प्रतीक है, का इच्छुक हो उसे अनिवार्यतः हत्या और रक्तपात से अपना हाथ रोक लेना चाहिए। और जिस किसी को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि वह अत्याचार और नाहक़ रक्तपात से बाज़ रहे वह निस्संदेह परिणामदर्शी और सौभाग्यशाली है।
(3) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि आप उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार रखते हैं जो अच्छा कर्म करता है और लोग उसके कारण उसकी प्रशंसा करते हैं। एक हदीस के शब्द ये हैं कि उस (नेक कर्म) के कारण लोग उससे प्रेम करते हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"यह तो मोमिन के लिए नक़्द और तात्कालिक शुभ सूचना है।" (हदीस : (मुस्लिम)
व्याख्या : ख्याति-मोह के निन्दनीय होने के कारण सहाबा को यह आशंका हुई कि नेक और अच्छे कर्म पर किसी की प्रशंसा करने या उससे प्रेम करने के कारण कहीं वह नेक कर्म अकारथ न जाए और आख़िरत में उसे उसका कोई प्रतिदान और सवाब तुम्हें प्राप्त न हो सके और कह दिया जाए कि तुम्हें अपने कर्म का बदला दुनिया में मिल चुका है, आख़िरत में उसका कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए सहाबा ने इस सिलसिले में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इसे स्पष्ट कराना चाहा।
मालूम हुआ कि यह तो एक नक़्द और तात्कालिक प्रतिदान है जो ईश्वर के अनुग्रह से शुभ सूचना के रूप में मोमिन को प्राप्त होता है। यह वास्तव में उस बन्दे के प्रशंसनीय और प्रिय होने का एक शुभ लक्षण है। यह शुभ सूचना तो फ़ौरन प्राप्त हो जाती है। वास्तविक प्रतिदान और सवाब जो योजना के तहत उसके लिए निश्चित है, वह अपनी जगह सुरक्षित है और वह उसे पारलौकिक जीवन में प्राप्त होगा। इस नक़द इनाम के कारण न तो उसका कर्म व्यर्थ होगा और न इससे उसके सवाब में किसी प्रकार की कोई कमी की जाएगी। कर्म के पीछे अगर निष्ठा कार्यरत हो तो इस प्रकार की चीज़ों से किसी का कर्म कभी अकारथ नहीं जाता।
पाखण्ड और कृत्रिमता
(1) हज़रत अबी-सअलबा ख़ुश्नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें मुझे सर्वाधिक प्रिय और मुझसे सर्वाधिक निकट क़ियामत के दिन वे लोग होंगे जो नैतिकता की दृष्टि से तुममें सबसे अच्छे हैं। और तुममें मुझे सर्वाधिक अप्रिय और सर्वाधिक मुझसे दूर वे लोग होंगे जो तुममें नैतिकता की दृष्टि से बुरे हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें बनानेवाले और बिना सावधानी और परहेज़ के बातों को तूल देनेवाले और दम्भ से मुँह फुला-फुलाकर बातें करनेवाले हैं।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : इस हदीस से ज्ञात हुआ कि किसी की व्यर्थ बकवास और लम्बे-चौड़े निरर्थक वार्तालाप और बातचीत में अनावश्यक कृत्रिमता इस बात का प्रमाण है कि वह नैतिकता की दृष्टि से अत्यन्त गिरा हुआ व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की निगाह में सबसे अधिक बुरा होगा। फिर उसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की संगति और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सामीप्य कैसे प्राप्त हो सकेगा।
स्वार्थपरता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ की माँग न करे कि उसके प्याले को ख़ाली कर दे और स्वयं विवाह कर ले, क्योंकि उसे वही मिलेगा जो उसके लिए नियत है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात औरत विवाह के लिए किसी के सामने यह शर्त हरगिज़ न रखे कि तुम पहले अपनी बीवी को तलाक़ दे दो तो मुझसे शादी रचा सकते हो। यह अत्यन्त स्वार्थपरता और निर्दयता की बात होगी जिसकी इस्लाम में क़तई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए यह बिल्कुल जायज़ नहीं है कि उससे उसके पति को छीन ले और इस प्रकार उसका हक़ मारकर सब कुछ अपने लिए समेट ले।
वह निकाह करना चाहती है तो कर ले, जो कुछ उसके लिए नियत है वह उसको मिलकर रहेगा। इसलिए अपनी मुसलमान बहन को हानि पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मनोदासता
(1) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब अपने पिता से वे अपने दादा से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
"इस उम्मत का प्रथम सुधार विश्वास और सांसारिक अमोह के कारण हुआ और उसका पहला बिगाड़ कृपणता और दीर्घ आशाओं के कारण होगा।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : इस हदीस में मुस्लिम समुदाय के सुधार और कल्याण के वास्तविक रहस्य और उसके बिगाड़ के मूल कारण पर रौशनी डाली गई है जिसकी उपेक्षा करके उम्मत न कभी सफलता प्राप्त कर सकती है और न बिगाड़ और उपद्रव से अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। विश्वास और सांसारिक अमोह जब तक इस उम्मत का सामूहिक चरित्र न हो वह कभी न तो अपने वास्तविक पद पर बनी रह सकती है और न उस दायित्व का यथोचित निर्वाह कर सकती है जो ईश्वर की ओर से उसे सौंपा गया है।
सांसारिक अमोह वास्तव में विश्वास और आस्था का प्रतिफल होता है। आदमी का विश्वास जितना अधिक ईश्वर और उसके किए हुए वादों पर और अन्तिम दिन की सफलताओं पर बढ़ता जाता है, उतना ही अधिक दुनिया और उसके भौतिक लाभ उसकी दृष्टि में तुच्छ होते जाते हैं। उसकी दृष्टि में वास्तविक चीज़ ईश्वर की प्रसन्नताप्राप्ति या फिर चारित्रिक उच्चता होती है। जिन व्यक्तियों में विश्वास और आस्था और सांसारिक अमोह जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं उनको सत्य से विचलित करना सम्भव नहीं रहता। वे प्रत्येक भय और लोभ-लिप्सा से निरपेक्ष रहते हुए सन्मार्ग पर गमन करते हैं। चारित्रिक मादकता और आनन्द उनकी वास्तविक निधि होती है जो उन्हें प्रत्येक वस्तु से निरपेक्ष रखती है।
कृपणता और दीर्घ आशाएँ वास्तव में आस्था, संयम और सांसारिक अमोहकता के प्रतिकूल हैं। जिन लोगों में कृपणता का रोग पाया जाता हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा जीने की अभिलाषा और आकांक्षा में मरे जाते हों उनका चरित्र ऐसा कभी नहीं हो सकता जो धर्म में अपेक्षित है, और जिसमें जान-माल की क्षति की सम्भावना भी हो सकती है। जब मुस्लिम समुदाय में कृपणता और लोभ-लिप्सा का रोग प्रवेश कर जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बरबादी और तबाही के दिन निकट आ गए हैं। उस तबाही से बचने का एक उपाय यह होता है कि उम्मत के अन्दर से इस नैतिक रोग को दूर किया जाए और उसके अन्दर चारित्रिक उच्चता का पुनरुत्थान किया जाए।
(2) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिन चीज़ों का मुझे उम्मत के लिए भय और आशंका है उनमें इन दो से मुझे डर है : स्वेच्छाचारिता और दीर्घाशा। स्वेच्छाचारिता सत्य से दूर रखती है और दीर्घाशा आख़िरत को भुला देती है। और ये दुनिया कूच करनेवाली, जानेवाली है और ये आख़िरत आगे बढ़नेवाली, आनेवाली है। और इन दोनों में से हरेक के पुत्र हैं। अगर तुमसे हो सके कि तुम दुनिया के पुत्र न हो तो ऐसा करो क्योंकि आज तुम कर्मभूमि में हो जहाँ हिसाब नहीं, लेकिन कल तुम परलोकगृह में होगे। वहाँ कर्म का अवसर नहीं होगा।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
व्याख्या : स्वेच्छाचारिता और दीर्घाशाओं से हमें सबसे अधिक बचना चाहिए। यूँ तो अन्य दुर्गुण भी हैं लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके परिणाम अत्यन्त भयावह और घातक होते हैं। स्वेच्छाचारी व्यक्ति को सत्य और असत्य की कोई परवाह नहीं होती। उसे तो केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाएँ और उद्देश्य ही प्रिय होते हैं। वह संसार में अधिक से अधिक वास करने और सांसारिक लाभों से अधिक से अधिक लाभान्वित होने की चिन्ता में जीता है। वह नहीं समझता कि जीवन का इससे भी उच्च कोई उद्देश्य हो सकता है। वह नहीं जानता कि आख़िरत और उसकी सफलता भी कोई चीज़ है जिसे प्राप्त करने की उसे चिन्ता करनी चाहिए। स्वेच्छाचारिता उसकी चिन्तनशक्ति को हर लेती है। वह मात्र इच्छा का दास होकर रह जाता है। मनेच्छाएँ जिस ओर भी उसे हाँक ले जाएँ वह निस्संकोच उस दिशा में चल पड़ता है। चाहे इससे उसके नैतिक अस्तित्व का अन्त ही हो जाए। उसे इसकी कोई चिन्ता नहीं होती। स्वेच्छाचारिता, स्वार्थपरता और आत्मोत्सर्ग से परहेज़, यही उसका चरित्र होता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन का कि “दोनों में से हरेक के पुत्र हैं" अर्थ यह है कि दुनिया और आख़िरत दोनों में से इनसान मूलतः किसी एक ही को चुन सकता है। क्योंकि दोनों में से हरेक की यह अपेक्षा होती है कि आदमी उसी का होकर रहे। अब विवेक और दूरदर्शिता यह है कि आदमी दुनिया का पुत्र अर्थात उसके अधीन होकर न रहे बल्कि दुनिया में रहकर मूल चिन्ता उसे आख़िरत की होनी चाहिए। यद्यपि संसार से प्रेम करनेवाले उसके पुत्र संख्या में बहुत हैं लेकिन उसे कदापि ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमेशा यह बात सामने रखने की है कि दुनिया की वास्तविक हैसियत कर्मभूमि की है। यह प्रतिफल-लोक या आनन्दगृह नहीं है। प्रतिफल-लोक तो वास्तव में आख़िरत है। दुनिया में जीवन का हिसाब नहीं देना होता लेकिन आख़िरत में हमें अपने समस्त कर्मों की जवाबदेही करनी होगी। फिर अपने कर्मों के अनुरूप हम वहाँ पुरस्कार या दण्ड के भागी होंगे।
फिर आख़िरत कोई दूर भी नहीं है। शीघ्र ही हम उससे दोचार होनेवाले हैं। यह दुनिया जिसपर लोग जान छिड़कते हैं, नश्वर और बीत जानेवाली है। इसके विपरीत आख़िरत की दुनिया जिसकी ओर ज़िन्दगी का कारवाँ रवाँ-दवाँ है, एक शाश्वत लोक है, जो अस्थायी और नश्वर जगत् कदापि सिद्ध न होगा।
लोभ-लिप्सा
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
"अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियाँ भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : सही बुख़ारी की एक दूसरी हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अगर आदम की सन्तान को सोने से भरी एक घाटी दे दी जाए तो वह दूसरी की इच्छा करेगा और अगर उसे दूसरी भी मिल जाए तो वह तीसरी का इच्छुक होगा। और आदम की सन्तान के पेट को तो मिट्टी ही भर सकती है।"
इस हदीस से मालूम हुआ कि धन-सम्पत्ति की भूख का कोई अन्त नहीं है। आदमी को कितनी ही दौलत क्यों न मिल जाए, तद्धिक की इच्छा शेष ही रहती है यहाँ तक कि वह मरकर मिट्टी में मिल जाता है। अलबत्ता जो लोग ईश्वर की ओर पलटते और उसकी कृपा छाया में आश्रय लेते हैं ईश्वर की उनपर विशेष अनुकम्पा होती है। वे अपने प्रभु को पाकर प्रत्येक चीज़ से बेपरवाह हो जाते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता उनके लिए संसार और संसार की समस्त वस्तुओं से बढ़कर प्रिय होती है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "दीनार और दिरहम और क़तीफ़ा और ख़मीसा का बन्दा हलाक हो। अगर उसे ये चीज़ें मिलती हैं तो वह प्रसन्न हो जाता है और अगर नहीं मिलती हैं तो प्रसन्न नहीं होता।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : क़तीफ़ा और ख़मीसा रेशमी चादर और ऊनी कपड़े हैं। एक हदीस में "और अगर नहीं मिलतीं तो क्रुद्ध होता है" के शब्द मिलते हैं।
इस हदीस का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक धन-सम्पत्ति का पुजारी है, उसके भाग्य में हलाकत के सिवा कुछ नहीं आता। वह भौतिक वस्तुओं के कारण महानता के उच्चासन से गिर जाता है। आश्चर्य की बात है कि उसकी प्रसन्नता और व्याकुलता भौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर करती है। हालाँकि आदमी के सुख-चैन और प्रसन्नता का सम्बन्ध ईश्वर की प्रसन्नता से होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अगर उसका ईश्वर उससे राज़ी और प्रसन्न है तो काँटे भी उसके लिए फूल हैं और अगर इसके विपरीत उसका प्रभु उससे क्रुद्ध और अप्रसन्न है तो संसार का कोई भी सुख या सम्पत्ति क्यों न हो, वह उसके लिए किसी यातना से कम नहीं।
(3) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक व्यक्ति की डकार सुनी तो कहा, “अपनी डकार को छोटा रखो क्योंकि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह व्यक्ति होगा जो दुनिया में ख़ूब पेट भरकर खाता है।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : 'डकार को छोटा करो' अर्थात डकार न लो। इतना मत खाओ कि डकार लेने की नौबत आए। ख़ूब पेट भरकर खाना और डकारें लेना अचेतनता का लक्षण है। मोमिन को हर उस आदत से बचना चाहिए जो दुनिया के पुजारियों और ग़ाफ़िलों की आदत और ग़फ़लत में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी करनेवाली होती है। यह जीवन ग़फ़लत में गुज़ार देने के लिए नहीं प्रदान किया गया है। आदमी को बहुत-से कठिन चरणों से गुज़रना है। मृत्यु की घड़ी और फिर प्रतापवान और महान ईश्वर के सामने खड़े होने की घड़ी इतनी कठिन घड़ी है कि आदमी को सही तौर पर इसका विचार हो तो वह कभी भी बेपरवाह नहीं हो सकता। ईश्वर के सामने उत्तरदायी होने की यह धारणा उसे यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी कि वह परीक्षा की कठिन घड़ी में है। फिर वह कदापि असावधानी के साथ निश्चिन्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकता।
यह एक तथ्य है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ईश्वर से निर्भय और बेपरहवाह होकर जीवन व्यतीत करता है वह आख़िरत में बड़े घाटे में रहेगा। यहाँ ग़ाफ़िल व्यक्ति को अगर सिर्फ़ अपना पेट भरने ही की चिन्ता रहती है तो आख़िरत में वह तृप्त न हो सकेगा और यह उसकी ग़फ़लत और बेपरवाही का अनिवार्य परिणाम होगा।
(4) हज़रत अम्र-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर की सौगन्ध, मैं तुम्हारी दरिद्रता से नहीं डरता बल्कि मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का भय है कि दुनिया तुमपर कुशादा कर दी जाएगी जिस प्रकार से उन लोगों पर कुशादा की गई जो तुमसे पहले गुज़रे हैं और फिर तुम उसी प्रकार उसे बेहतर चाहने लगो जिस प्रकार तुमसे पहले के लोग उसकी चाहत और रसास्वादन में ग्रस्त हुए और यह कि दुनिया तुम्हें भी विनष्ट कर दे जिस प्रकार उसने उनको विनष्ट किया।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात दरिद्रता और निर्धनता के कारण आदमी फ़ित्नों और आज़माइशों में पड़ सकता है लेकिन इससे बढ़कर उसके बारे में आशंका तब होती है जब कि उसके लिए धन-सम्पत्ति के द्वार खुल जाएँ और वह दौलत की चाहत में अपने मौलिक दायित्वों को भुला बैठे। उसे धुन हो तो इस बात की कि कितनी जल्दी वह अपने लिए अधिक से अधिक धन एकत्र कर ले। वह लिप्सा का ऐसा दास बन जाए कि न उसे फ़क़ीरों और निर्धनों पर दया आए और न अपने धन को ईश्वरीय मार्ग में ख़र्च कर सके और अन्ततः ईश्वर का कोप-भाजन बनकर रहे, जिस प्रकार पिछली उम्मतें ईश्वरीय यातना की भागी हुई हैं।
यहाँ यह बात याद रहे कि आवश्यकता से बढ़कर जब किसी व्यक्ति के पास धन एकत्र हो जाता है तो इसकी बड़ी सम्भावना होती है कि कहीं वह दुनिया में इस प्रकार लीन होकर न रह जाए कि न उसे ईश्वर याद आए और न उसे आख़िरत ही की कोई चिन्ता हो और न दुनिया ही में विनष्ट हो जाने का उसे भय हो।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लोभ एवं कृपणता और ईमान किसी बन्दे के दिल में कभी एकत्र नहीं होते।” (हदीस : नसई)
व्याख्या : मुस्नद अहमद की एक हदीस है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"दो गुण ऐसे हैं जो किसी मोमिन में एक साथ नहीं पाए जा सकते। वे हैं कृपणता और दुःशीलता।”
सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से एक हदीस उल्लिखित हुई है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बचो अत्याचार से, क्योंकि अत्याचार से क़ियामत के दिन कालिमा छा जाएगी। और लोभ और कृपणता से बचो, क्योंकि लोभ और कृपणता ने तुमसे पहले लोगों को विनष्ट किया, उन्होंने इसके कारण रक्तपात किया और हराम को हलाल ठहरा लिया।"
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से कि "लोभ एवं कृपणता और ईमान किसी बन्दे के दिल में एकत्र नहीं होते" मालूम हुआ कि लोभ और कृपणता वास्तव में ईमान और उसकी अपेक्षाओं के प्रतिकूल हैं। ईमान का अर्थ यह है कि आदमी सांसारिक धन-सम्पत्ति का नहीं बल्कि ईश्वर का अनुरागी हो। अगर ईश्वर ने उसे धन-सम्पत्ति प्रदान की है तो वह उसे स्वयं तक ही सीमित न रखे बल्कि उसे बेसहारा लोगों और ईश्वर के धर्म की स्थापना पर भी व्यय करे। लेकिन लोभ और कृपणता में पड़ा हुआ व्यक्ति न अपनी दौलत को ईश्वरीय मार्ग में ख़र्च करता है। और न उसकी दौलत से निर्धनों को कोई लाभ पहुँच पाता है।
(6) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"आदम की सन्तान बूढ़ी हो जाती है मगर उसमें दो चीज़ें ज़्यादा जवान हो जाती हैं : धन-सम्पत्ति का लोभ और जीने की लालसा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : बुख़ारी और मुस्लिम में अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से एक हदीस उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों के सम्बन्ध में जवान ही रहता है। एक संसार से प्रेम और दूसरा दीर्घ आशाएँ और आकांक्षाएँ।”
साधारणतः देखने में यही आता है कि आदमी बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है लेकिन उसकी धन-लोलुपता, सांसारिकता और जीने की उसकी लालसा में कोई कमी नहीं आती। शरीरिक शक्ति क्षीण और शिथिल पड़ जाने के कारण इच्छाओं पर नियन्त्रण पाना भी उसके लिए आसान नहीं होता। उसकी इच्छाएँ वासनाओं का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन इससे ईश्वर के वे बन्दे सुरक्षित हैं जो सदैव परिणाम पर नज़र रखते हैं। वे सांसारिक जीवन और उसके साधनों को अस्थायी समझते हैं। जिन्होंने आख़िरत को दृष्टि में रखकर स्वयं को प्रशिक्षित किया हो वे नश्वर कामनाओं के विपरीत ईश्वर की प्रसन्नता और आख़िरत की अपार नेमतों के अभिलाषी होते हैं और वृद्धावस्था में भी उनके इस शौक़ और उल्लास में कोई कमी नहीं आती।
(7) हज़रत काब-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"दो भूखे भेड़िये जो बकरियों में छोड़ दिए जाएँ वे उन बकरियों को उससे बढ़कर तबाह नहीं करते जितना धन और प्रतिष्ठा के लिए आदमी का लोभ उसके धर्म को विनष्ट करके रख देता है।" (हदीसः तिर्मिज़ी, दारमी)
व्याख्या : धर्म क्या है? जीवन में ईश्वर को अपनाना। इस प्रकार जीवन व्यतीत करना कि आदमी का पूरा जीवन ईश्वरीय सौन्दर्य के अनुरूप बन जाए। उसके व्यक्तित्व और आचरण से साफ़ प्रकट हो कि वह ईश्वर के सौन्दर्य और प्रताप पर न्योछावर है। उसका सम्पूर्ण भक्तिभाव एक ईश्वर के लिए विशिष्ट होकर रह गया है। ऐसे व्यक्ति की हार्दिक कामना यह होती है कि वह ईश्वर के सामने अपने आप को आत्यान्तिक रूप से नत कर दे ताकि उसके प्रभु की उच्चता प्रकट हो। वह इस बात का इच्छुक होता है कि ईश्वर के प्रेम रस से वह इस प्रकार अभिभूत हो कि यह चीज़ उसे नश्वर वस्तुओं के प्रेम से विमुख कर दे। सत्य यह है कि जिस व्यक्ति को सही अर्थों में ईश्वर का ज्ञान हो गया उसकी दृष्टि में ईश्वर के मुक़ाबले में न कहीं और कोई प्रतिष्ठा और महानता है और न उसके मुक़ाबले में कहीं कोई सौंदर्य और आकर्षण पाया जाता है जिसके लिए उसका दिल विकल और बेचैन हो सके। यही वास्तविक धर्म है। अब अगर कोई आदमी सांसारिक धन-सम्पत्ति और सांसारिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का भूखा है तो स्पष्ट है कि वह धर्म और उसके आनन्द से नितान्त अपरिचित है। उसे अगर अपने सुधार का ध्यान नहीं होता तो उसके धर्म की तबाही में क्या सन्देह हो सकता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दो भूखे भेड़ियों और बकरियों की मिसाल धर्म की इस भयावह तबाही का एहसास दिलाने के लिए प्रस्तुत की है। भूखे भेड़िये बकरियों को कैसे जीवित छोड़ सकते हैं? ठीक इसी प्रकार धन-लोलुपता और पद-प्रतिष्ठा का लोभ दो भयानक भेड़ियों की भाँति हैं। ये आदमी के धर्म के लिए घातक सिद्ध होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा घातक जितने दो भूखे भेड़िये बकरियों के लिए घातक होते हैं।
(8) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक दिन भाषण दिया और उसमें कहा—
"लोभ-लिप्सा से बचो क्योंकि तुमसे पहले जो लोग गुज़रे हैं वे लोभ-लिप्सा ही के कारण तबाह हुए। उसी ने उन्हें कृपणता पर उभारा तो वे कृपणता में लिप्त हुए, उसी ने उन्हें नाते-रिश्ते तोड़ने पर उभारा तो उन्होंने नाते-रिश्ते तोड़े और उसी ने उन्हें अवज्ञाओं और उल्लंघनों पर उकसाया तो वे अवज्ञाकारी हुए।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : कृपणता या लालच से आदमी का धर्म किस प्रकार भ्रष्ट होता है और किस प्रकार यह चीज़ स्वयं उसके लिए भी घातक सिद्ध होती है इस हदीस से यह बात भली-भाँति स्पष्ट होती है। लोभ और संकीर्णता के कारण ही पिछली क़ौमों ने कृपणता को अपना स्वभाव बनाया और फिर इस कृपणता ने उन्हें प्रत्येक ज़ुल्म और सितम पर आमादा किया। उन्होंने अपने सगे-सम्बन्धियों और रिश्तेदारों तक के अधिकारों का हनन किया और इसके कारण वे प्रत्येक प्रकार के दुराचार और सीमोल्लंघन में लिप्त हुए और अन्ततः वे ईश्वरीय कोप का भाजन बनकर रहे।
(9) हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदम के पुत्र के हृदय के लिए हरेक घाटी और मैदान में एक शाखा है। अतएव जो व्यक्ति उनमें से हरेक शाखा (इच्छा) के पीछे अपने दिल को लगाएगा तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह न होगी कि उसे किस घाटी में विनष्ट करे, और जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उन समस्त शाखाओं के मामले में उसके लिए काफ़ी हो जाएगा।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : मानव-मन की इच्छाएँ और वासनाएँ हर क्षेत्र में फैली हुई हैं। अब अगर आदमी उन इच्छाओं के पीछे पड़ेगा, उन्हें ही अपना मूल उद्देश्य बनाएगा और अपने विचार के घोड़े हर दिशा में दौड़ाता फिरेगा तो ईश्वर अपनी रक्षा से उसे अलग कर देगा। उसे इसकी कोई परवाह न होगी कि वह कहाँ तबाह और बरबाद होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर वह ईश्वर पर भरोसा करके सीधे रास्ते पर चलने का प्रयास करता है और उसकी बन्दगी में लगा रहता है तो न केवल यह कि ईश्वर उसके धर्म एवं ईमान और नैतिकता की रक्षा करेगा बल्कि उसकी समस्त आवश्यकताओं के मामले में भी वह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ईश्वर उसे ऐसी शान्ति और परितोष प्रदान करेगा जिससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है।
संसार-प्रेम
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शीघ्र अति शीघ्र नेक काम कर लो, उस फ़ित्ने से पहले जो अन्धेरी रात के टुकड़े जैसा (अन्धकारमय) होगा। सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफ़िर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफ़िर। वह अपने धर्म को सांसारिक सामग्रियों के बदले बेच डालेगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : फ़ितना जो अन्धेरी रात के टुकड़े जैसा होगा अर्थात यह फ़ितना रौशनी को निगल लेने को आतुर होगा। कोई व्यक्ति सुबह को मोमिन होगा लेकिन यह नहीं कहा जा सकेगा कि वह शाम तक मोमिन रह भी सकेगा या नहीं। इसी प्रकार एक व्यक्ति शाम को मोमिन होगा लेकिन इसकी कोई गारंटी न होगी कि वह आनेवाली सुबह को भी मोमिन रह सके। ऐसा इनक़िलाब आएगा कि कोई प्रातः समय मोमिन तो सन्ध्या को काफ़िर होगा या सन्ध्या को मोमिन तो प्रातःकाल उसके लिए कुफ़्र (अधर्म) का सन्देश बनकर आएगा। ईमान में कोई दृढ़ता न होगी। लोग चारित्रिक उच्चता से रहित होंगे।
उस समय दुनिया की लालसा ऐसी छाई हुई होगी कि लोगों के दिलों में धर्म का कोई मूल्य शेष न रहेगा। सांसारिक हितों के लिए लोग अपने धर्म तक का सौदा करेंगे। उन्हें दुनिया प्राप्त करने के लिए अपने धर्म को बेच देने में कोई संकोच या लज्जा न होगी।
(2) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"निस्सन्देह यह माल हरा, रुचिकर, ताज़ा और स्वादिष्ट है। अतः जो व्यक्ति इसे जायज़ तरीक़े पर प्राप्त करे और जायज़ कामों में ख़र्च करे तो यह माल सबसे अच्छा सहायक है और जो व्यक्ति इसको नाजायज़ तरीक़े से प्राप्त करे तो वह उस व्यक्ति की तरह होता है कि जो खाता है और अघाता नहीं, और यह माल क़ियामत के दिन उसका साक्षी होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह वास्तव में एक लम्बी हदीस का एक अंश है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कहने का अर्थ यह है कि दुनिया का माल इनसान के लिए स्वादिष्ट भी होता है और अच्छा भी। बुद्धिमान वह है जो जीवनोद्देश्य के सम्बन्ध में इसे अपना सहायक बनाता है। माल को जायज़ तरीक़े से प्राप्त करता है और उसे जायज़ कामों में ख़र्च करता है। माल की उसे चिन्ता होती है तो बस आवश्यकता भर होती है। अधिक से अधिक दुनिया समेटने के लोभ में वह कभी नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो कोई माल की प्राप्ति और उसके उपयोग में उचित-अनुचित की परवाह नहीं करता वह वास्तव में धन का पुजारी है। धन ही उसका जीवन-लक्ष्य है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी तृप्ति और परितोष धन प्राप्त नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल क़ियामत में यह स्पष्ट होकर रहेगा कि उसके जीवन में जीवन के उच्च अर्थ का अभाव ही रहा। दुनिया का धन ही उसके लिए सब कुछ था। वह धन के प्रेम में ऐसा लिप्त रहा कि उसे इसका अवकाश ही न मिला कि वह जीवन में अपने वास्तविक दायित्व को महसूस कर सकता। वह जीवन की अन्तिम साँस तक धनलोलुप ही बना रहा। और यह लोलुपता ऐसी थी जो समाप्त होनेवाली न थी। अन्ततः मृत्यु ने उससे वह सब छीन लिया जिसपर वह जान छिड़कता रहा है। जिस बड़े सत्य से उसे दोचार होना था उसकी उसे चिन्ता न हो सकी। धन जो जीवन के मूल लक्ष्य अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति में उसका सहायक हो सकता था वह उसके लिए मुसीबत और आफ़त बनकर रहा। उसके हाथ ग्लानि और सन्ताप के सिवा कुछ और न आ सका। क़ियामत में इसका भी अवसर न होगा कि वह क्षतिपूर्ति कर सके।
(3) हज़रत काब-बिन-अयाज़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“प्रत्येक उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात प्रत्येक क़ौम की ईश्वर ने किसी न किसी चीज़ के द्वारा परीक्षा ली है। इस मुस्लिम समुदाय की परीक्षा विशेषतः धन के द्वारा होगी। अगर कोई व्यक्ति भौतिक लाभ ही को सब कुछ समझता है और धन-प्रेम से ग्रसित होकर रहता है और धन-प्राप्ति ही को अपनी सफलता समझता है तो इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि यह धन उसके लिए ऐसी परीक्षा सिद्ध हुआ जिसमें वह असफल रहा।
इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वास्तव में अपनी उम्मत को सचेत किया है कि यद्यपि इस उम्मत को 'यौमुस्सब्त' (सप्ताह के दिन) की आज़माइश जैसी आज़माइश नहीं होगी और न सामरी के फ़ितने जैसा कोई फ़ितना खड़ा होगा, लेकिन माल का फ़ितना स्वयं एक बड़ा फ़ितना है जिससे उसे गुज़रना पड़ेगा। माल की मुहब्बत में पड़कर आदमी अकसर अपने ईमान और विश्वास की अपेक्षाओं को भुला देता है और ईश्वर की दृष्टि में अत्याचारी ठहरता है। इस उम्मत की सफलता इस पर निर्भर करती है कि यह दुनिया को दुनिया समझे और अपनी दृष्टि हमेशा पारलौकिक कल्याण और आख़िरत में प्राप्त होने वाली सफलताओं पर जमाए रखे। सांसारिक धन-सम्पत्ति के प्रेम के साथ यह उम्मत कभी भी उस दायित्व का यथोचित निर्वाह नहीं कर सकती जो ईश्वर ने उसके सुपुर्द की है, अर्थात स्वयं सन्मार्ग पर चलना और संसारवालों को सत्य की ओर आमन्त्रित करना और इस सम्बन्ध में नेतृत्व का दायित्व निभाना। यह ऐसा दायित्व है जिससे वह किसी हालत में भी मुक्त नहीं हो सकता।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सावधान, दुनिया तिरस्कारयोग्य है और जो कुछ दुनिया में है वह भी तिरस्कारयोग्य है। सिवाय ईश्वर के स्मरण और उस चीज़ के जिसे ईश्वर पसन्द करता है और विद्वान या विद्यार्थी के।” (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : अर्थात यह दुनिया और इसकी चीज़ें मूल्यहीन और तुच्छ हैं। ये इनसान का लक्ष्य नहीं हो सकतीं। मिट जानेवाली दुनिया ऐसी चीज़ नहीं जिसपर कोई सन्तुष्ट हो सके। आदमी की अभिलाषाओं का केन्द्र तो आख़िरत की दुनिया ही हो सकती है जो हमेशा बाक़ी रहने वाली होगी, जहाँ की बहारों को पतझड़ का भय नहीं। दुनिया की मनोरमताएँ अकसर भ्रम सिद्ध होती हैं। उनमें पड़कर अकसर लोग ईश्वर से ग़ाफ़िल हो जाते हैं। इस पहलू से भी मर्मज्ञों की दृष्टि में इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस दुनिया में अगर मूल्यवान कोई चीज़ है तो वह ईश-स्मरण और ईश-महानता का ज्ञान है। या वे चीज़ें जिन्हें ईश्वर पसन्द करे, जैसे बन्दगी और आज्ञापालन, सच्चरित्रता और सत्कर्म। या फिर वह विद्वान जो ईश्वर को पहचानता है और लोगों में ईश-भक्ति की भावना का संचार करने के प्रयास में लगा रहता है या वह व्यक्ति जो सत्यज्ञान की खोज में रहता है।
इस हदीस में "ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु" आया है। 'व मा वालाहु' का एक अर्थ तो वह है जो हमने अनुवाद में लिया है। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, “वे चीज़ें जो ईश्वर के स्मरण के निकट और उसके सदृश हों।" और इसका तीसरा अर्थ यह भी सम्भव है, "वे चीज़ें जो ईश्वर के स्मरण की अपेक्षाओं और अनिवार्यताओं के अन्तर्गत आती हों।"
(5) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी चीज़ से तेरा प्रेम तुझे अन्धा और बहरा बना देता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने संक्षिप्त शब्दों में बड़ी चेतावनी दी है और मानव को उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी से अवगत कराया है। आदमी की यह सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जब उसके दिल में किसी चीज़ का प्रेम घर कर जाता है तो उसके अवगुण भी उसे गुण प्रतीत होने लगते हैं। वह इस अवस्था में नहीं रहता कि सत्य और असत्य में अन्तर कर सके और केवल सत्य का समर्थन करे और असत्य को अस्वीकार कर दे।
इसलिए इनसान के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह गम्भीरतापूर्वक इसका निर्णय ले कि इस जीवन में क्या चीज़ है जिससे वह जी लगाए और कौन-सी चीज़ है जिससे उसको बेपरवाह होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि उसके लिए वह कौन-सी चीज़ हो सकती है जिसकी तलब में वह सक्रिय हो इसलिए कि अगर वह कहीं ऐसी चीज़ का अभिलाषी हो गया हो जो इस बात के योग्य न थी कि आदमी उसका अभिलाषी हो तो फिर बाद में उससे पीछा छुड़ाना सरल न होगा।
आदमी का व्यक्तित्त्व तीन चीज़ों से निर्मित होता है। उसके कुछ विचार और धारणाएँ होती हैं। इसी प्रकार उसकी कुछ भावनाएँ होती हैं जिनकी वह तुष्टि और पूर्ति चाहता है। और फिर उसकी कर्मशक्ति होती है जो अपने लिए क्षेत्र का चुनाव करती हैं। इन तीनों ही पहलुओं से धर्म ने जो मार्गदर्शन किया है वह सही और दुरुस्त हो सकता है।
अच्छी और ऊँची धारणाएँ वही हैं जिनकी शिक्षा हमें किताब और सुन्नत में मिलती है। इसलिए उन्हीं धारणाओं को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी धारणाएँ और विचारधाराएँ जो इस्लामी विचारधाराओं के विरुद्ध हैं, कभी भी ध्यान देने योग्य नहीं हो सकतीं। आदमी को पहले ही क़दम पर यह जान लेना चाहिए कि ग़ैर-इस्लामी विचारधाराएँ उसे एक ऐसे मरुस्थल में ला खड़ा करेंगी जहाँ न कोई छाया होगी और न ठंडक का कोई सामान। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो मुस्लिम घराने में जन्म लेने पर भी मार्क्सवादी विचारों के ऐसे अनुरागी हुए कि उन्हें वही विचार सबमें श्रेष्ठतर और वैज्ञानिक नज़र आने लगे और फिर वे अपने विरुद्ध अत्यन्त बुद्धिसंगत तर्कों पर भी ध्यान देने को तैयार न हुए।
भावनाओं और अनुभूतियों को देखिए। आदमी अगर सस्ती क़िस्म की भावनाओं का आदी हो गया तो फिर उसे वे भावनाएँ जो अत्यन्त पवित्र और सूक्ष्म हैं, नीरस मालूम होंगी। वह मानव की गहरी मानसिकता और वास्तविक प्रकृति से अपरिचित ही रहता है। भक्तिभाव हो या ईश-प्रसन्नता की इच्छा, संयम व ईशभय हो या दूसरों की भलाई और हित चाहने की भावना और ख़ुदा और रसूल से प्रेम, जीवन के इन उच्च मूल्यों और मान्यताओं से उसे कोई हार्दिक लगाव नहीं होता और न उसे इनमें उस मिठास की प्रतीति होती है जो हृदयों के लिए आहार तुल्य है।
इसी प्रकार जीवन के व्यावहारिक पक्ष को लीजिए। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष सभ्यता का अनुरागी हो जाता है तो फिर वह उसी का समर्थक बनकर उठेगा। उसे इस्लामी सभ्यता और इस्लामी जीवन-व्यवस्था में कोई आकर्षण सिरे से नज़र ही नहीं आ सकता।
ऐसा व्यक्ति अन्धा भी बन जाता है और बहरा भी हो जाता है। न वह देख सकता है कि वह स्वयं गुण-अवगुण का विश्लेषण कर सके और न किसी की सुन ही सकता है कि सुनकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सके।
कितने ही लोग हैं जो दुनिया और उसकी साज-सज्जा पर ऐसे मोहित हुए कि उन्हें इस प्रत्यक्ष जगत् के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता। इस नश्वर जगत् का सौन्दर्य ही उनके लिए सब कुछ है। सांसारिक साज-सज्जा ही उनकी तलब का हासिल होता है। सांसारिक ख्याति और नामवरी प्राप्त करना ही उनके लिए वास्तविक जीवन-साध्य है। उनकी संकीर्णता पर आप जितना भी मातम करें कम है, मगर इनसान की इस कमज़ोरी को क्या कीजिए कि आदमी की अपनी चाहत उसे अन्धा और बहरा बनाकर छोड़ती है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन की सत्यता को हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। कभी आदमी को अपनी सन्तान से इतना प्रेम हो जाता है कि वह दुराचारी और ईश-द्रोही ही क्यों न हो तो भी उसे उससे घृणा नहीं होती। कभी आदमी क़ौमी पक्षपात और क़ौम के प्रेम में इस प्रकार ग्रसित होकर रह जाता है कि उसकी सारी सहानुभूतियाँ और संवेदनाएँ अपनी ही क़ौम और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर रह जाती हैं। दूसरे लोगों के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। क़ौम सत्य पर हो या असत्य पर, वह प्रत्येक हालत में अपनी क़ौम के समर्थन में लगा रहेगा। जबकि क़ुरआन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—
“और जो ईमानवाले हैं उन्हें सबसे बढ़कर प्रेम अल्लाह से होता है।" (2:165)
ईमानवालों के प्रेम का केन्द्र बिन्दु ईश्वर ही होता है। उनकी सारी मित्रता और शत्रुता और उनके जीवन की सारी दौड़-धूप बस उसी एक प्रेम के अधीन होती है।
(6) हज़रत क़तादा-बिन-नोअ्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब अल्लाह किसी बन्दे से प्रेम करता है तो वह उसको दुनिया से इस प्रकार बचाता है जिस प्रकार तुममें से कोई अपने बीमार को पानी से परहेज़ कराता है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर अपने प्रिय बन्दे को नष्ट होने से बचाता है। वह उसका रक्षक बन जाता है। जिस बन्दे को ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त होती है, वह संसार के प्रेम में नहीं पड़ता। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस बात को एक मिसाल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय सम्बन्धी को ऐसे रोग में जिसमें पानी हानिकर होता है, पानी से बचाता है और उसे पानी पिलाने में अत्यन्त सावधानी से काम लेता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपने प्रिय और वफ़ादार बन्दों को दुनिया के प्रेम और उसकी उन चीज़ों से दूर रखता है जिनसे उनके धर्म को हानि पहुँचने की आशंका होती है और जिनसे उनका परलोक ख़तरे में पड़ सकता है।
(7) हज़रत सौबान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जल्द ही ऐसा होगा कि क़ौमें तुमपर टूट पड़ेंगी जिस प्रकार खाने वाले एक-दूसरे को खाने के प्याले की तरफ़ बुलाते हैं।" एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि “और ऐसा उस समय हमारे अल्पसंख्यक होने के कारण होगा?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“नहीं, तुम तो उस युग में बड़ी संख्या में होगे लेकिन तुम्हारी हैसियत कूड़े-करकट की होगी, जैसे वह कूड़ा जो नदी और बाढ़ के झाग के साथ मिला हुआ होता है। अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं के दिलों से तुम्हारा भय निकाल देगा। और तुम्हारे दिलों मे ‘वहन' डाल देगा।” एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! वहन क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "संसार का मोह और मृत्यु का नागवार होना।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय की शक्ति और सामर्थ्य का वास्तविक रहस्य क्या है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने प्रारम्भ ही में मुसलमानों को सचेत कर दिया है कि जब तक उनका अपने जीवन-उद्देश्य से प्रेम का नाता रहेगा और वे उसके लिए हर प्रकार का त्याग करने को अपने सम्पूर्ण हृदय से तत्पर रहेंगे, कोई भी क़ौम उनपर बेबाकाना हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। लेकिन जिस समय ईमानवाले संसार-प्रेम में लिप्त हो जाएँगे और मृत्यु उनके लिए नागवार हो जाएगी, उस समय उनकी धाक ख़त्म हो जाएगी। विरोधी क़ौमें उनको अपना सहज ग्रास बना लेंगी। उनपर शत्रु चढ़ दौड़ेंगे। मुसलमानों को दूसरी क़ोमों की तुलना में अगर वरीयता प्राप्त हो सकती है और वे कर्मभूमि में सब पर बाज़ी ले जा सकते हैं तो इस तरह कि वे दुनिया को अपना जीवन लक्ष्य न समझें और ऐसी मृत्यु को जो ईश्वरीय आज्ञापालन और बन्दगी के मार्ग में आए, उसे वे अपने लिए बड़ी सफलता समझें।
भोग-विलास
(1) हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्हें गवर्नर बनाकर यमन भेज रहे थे तो उस अवसर पर कहा—
“तुम भोग-विलास में पड़ने से स्वयं को बचाना क्योंकि अल्लाह के बन्दे विलासी नहीं होते।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात तुम यमन में एक शासक के रूप में जा रहे हो। वहाँ जीवन की सुख-सामग्रियों और भोग-विलास से फ़ायदा उठाने के अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, मगर तुम सांसारिक शासकों की नीति कदापि न अपनाना। ईश्वर के वफ़ादार बन्दों को मूल चिन्ता उस दायित्व को पूर्ण करने की होनी चाहिए जो ईश्वर ने उनपर डाला है।
यह दुनिया ऐसी जगह नहीं है कि आदमी यहाँ विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने की चिन्ता में लीन हो। जीवन तो बस आख़िरत का जीवन है।
(2) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमें सोने-चाँदी के पात्रों में खाने-पीने और रेशम और दीबा का लिबास पहनने और उसपर बैठने से मना किया है। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थ यह है कि अमीराना ठाठ-बाट और ईरान-तूरान आदि की साज-सज्जा और विलासिता का इस्लामी जीवनशैली से कोई सरोकार नहीं है। मोमिन के लिए इस प्रकार की चीज़ों से बचना अनिवार्य है।
(3) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे कहा—
“(घर में) एक बिस्तर पुरुष के लिए और एक बिस्तर स्त्री के लिए होता है और तीसरा अतिथि के लिए होता है और चौथा शैतान के लिए।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात इस्लाम भोगविलास और अपव्ययी जीवन को पसंद नहीं करता। घर में सामान ज़रूरत भर अवश्य होना चाहिए। अनावश्यक फ़र्निचर, क़ालीनों और दूसरी वैभवपूर्ण सामग्रियों की अधिकता इस बात का सबूत है कि शैतान ने आदमी को जीवन के मूल उद्देश्य से विमुख कर रखा है।
इस हदीस का आशय सामान और बिस्तर आदि की संख्या निर्धारित करना नहीं है बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य उस मानसिकता का परिष्कार है जिससे आदमी के अन्दर सांसारिकता या संसारिक इच्छाओं के प्रति मोह उत्पन्न होता है। किसी के यहाँ अगर अतिथियों का बाहुल्य है तो इस स्थिति में बिस्तर आदि की अधिकता कोई बुरी बात न होगी।
निर्लज्जता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा का सम्बन्ध ईमान से है और ईमान का परिणाम स्वर्ग है और निर्लज्जता का सम्बन्ध स्वभाव की कठोरता से है और स्वभाव की कठोरता का परिणाम नरक है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात मोमिन लज्जावान होता है। लज्जा ईमान का लक्षण है और ईमान का एक छोर स्वर्ग से मिला हुआ है। ईमानवालों की मंज़िल स्वर्ग ही होगी।
इसके विपरीत निर्लज्जता आदमी के कठोर हृदय होने का प्रमाण होती है। स्वभाव की कठोरता अंततः उसे ले डूबेगी। ऐसा व्यक्ति जीवन के वास्तविक आनन्द से अपरिचित ही रहता है। और स्वभाव की यही कठोरता उसके नरक में जा पहुँचने का कारण बन जाती है।
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस चीज़ में अश्लीलता और निर्लज्जता की बात होती है वह अनिवार्यतः उसे ऐबदार और कुरूप बना देती है और लज्जा और शर्म जिस चीज़ में होती है वह अनिवार्यतः उसे सुन्दर बना देती है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह एक तथ्य है कि लज्जा सर्वथा सौन्दर्य और निर्लज्जता सर्वथा कुरूपता और अवगुण है। किसी व्यक्ति में लाख गुण हों लेकिन अगर वह बेशर्म और बेग़ैरत है तो उसके समस्त गुणों पर पानी फिर जाएगा और वह हर किसी की निगाह से गिर जाएगा। इसके विपरीत लज्जा जहाँ और जिस रूप में भी पाई जाएगी सौन्दर्य और शोभा ही बढ़ाएगी। निस्सन्देह लज्जा ज़िन्दगी की शोभा और नैतिकता एवं सामाजिकता का सौन्दर्य है।
(3)
अधमता और नीचता
क्षुद्र मानसिकता
(1) हज़रत अबुल-अहवस (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता से उल्लेख करते हैं कि उनका बयान है कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय मेरे शरीर पर अत्यन्त ख़राब और मामूली कपड़े थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझसे कहा—
“क्या तुम्हारे पास माल है?” मैंने कहा, “जी हाँ।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "किस प्रकार का माल है?" मैंने कहा कि अल्लाह ने मुझे प्रत्येक प्रकार के माल से सम्पन्न किया है। ऊँट, गायें, बकरियाँ और घोड़े भी हैं और ग़ुलाम भी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जब ईश्वर ने तुझे धन प्रदान किया है तो ईश्वर की नेमत का और उसने तुझे जो इज़्ज़त दी है उसका प्रभाव भी दिखाई देना चाहिए।" (हदीस : नसई)
व्याख्या : मतलब यह है कि क्षुद्रता और अधोमानसिकता एक प्रकार से कृतघ्नता है। इससे बचना चाहिए। किन्तु ईश्वर की दी हुई नेमत के प्रकटीकरण में आदमी को इतना आगे भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि यह चीज़ अपव्यय और दिखावा मात्र बनकर रह जाए।
संकीर्णता और तंगदिली
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"कुछ देकर वापस लेनेवाला उस कुत्ते की भाँति है जो उल्टी करके उसे चाट लेता है। यह बुरी मिसाल कदापि हमपर चरितार्थ नहीं होनी चाहिए।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात मोमिन को यह कदापि शोभा नहीं देता कि कुछ देकर वह अकारण उसे वापस ले ले। यह अत्यन्त ही नीचतापूर्ण और घिनावनी बात होगी। मोमिन में किसी प्रकार की तंगी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उसके प्रतिष्ठानुकूल हो सकती है वह विशाल हृदयता है, न कि संकीर्णता और तंगदिली।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कृपणता और लोभ से बचो, क्योंकि इस कृपणता और लोभ ने तुमसे पहले के लोगों को विनष्ट किया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात कृपणता और लोभ-लिप्सा घातक है। पिछली क़ौमें भी इसी के कारण विनष्ट हुई हैं। और यह चीज़ जीवन के लिए आगे भी घातक सिद्ध हो सकती है। क़ुरआन में है—
“और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिये जाएँ ऐसे ही लोग सफल हैं।" (59:9)
कृपणता और संकीर्ण-हृदयता के कारण आदमी में नाना प्रकार की नैतिक गिरावटें उत्पन्न हो जाती हैं। पिछली क़ौमों में जब यह रोग फैल गया तो वे क़ौमें सांसारिकता में ग्रस्त होकर रह गईं। दुनिया ही को उन्होंने अपना मूल उद्देश्य समझ लिया। फिर इसका परिणाम यह हुआ कि लोग परस्पर एक-दूसरे के अधिकारों का भी हनन करने लगे। उनके मापदंड देने के और, लेने के और हो गए। लेते तो पूरा-पूरा लेते और देना होता तो कम तौलते। सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना उनके यहाँ निरर्थक होकर रह गई। फिर यह रोग इतना बढ़ा कि उनके लिए प्रत्येक सदुपदेश निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। अन्ततः तबाही और बरबादी और हलाकत से उन्हें कोई न बचा सका। ऐसी क़ौमों का जो परिणाम निश्चित है उसी से उनको दोचार होना पड़ा।
मानव-चरित्र को मूलतः जो वस्तु अपेक्षित होती है वह है विशाल-हृदयता और अनुभूति की सूक्षमता। अगर हमारे अन्दर ये चीज़ें नहीं हैं तो तथ्यात्मक दृष्टि से हम से बढ़कर दरिद्र कोई नहीं है। किसी व्यक्ति या राष्ट्र को जानने के लिए मूलतः जो चीज़ देखने की होती है वह यह नहीं है कि उसके पास कितना साज़ो-सामान और धन सम्पत्ति है, बल्कि देखने की चीज़ यह है कि वह व्यक्ति या राष्ट्र स्वयं क्या है? इस पहलू से हमें सर्वप्रथम स्वयं अपना निरीक्षण करना चाहिए। इनसान मात्र हाड़-माँस से बना कोई ढाँचा नहीं है बल्कि वह इसके सिवा कुछ और है। साधारणतः हमारी निगाहें इसी बाह्य ढाँचे पर टिककर रह जाती हैं। हम इसी को लाभ-हानि का वास्तविक मानदंड समझने की ग़लती कर जाते हैं। हम मानव-आत्मा को हमेशा अनदेखा करते रहते हैं जिसके तेज से स्वयं इस बाह्य अस्तित्व अर्थात शरीर की गरिमा भी बनी रहती है। इस भौतिक जगत् में आत्मा का पूर्णतः अनुभव तो मुश्किल है। लेकिन समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि मानव तथ्यतः एक नैतिक अस्तित्व है। अतएव उसकी आत्मा के स्वस्थ और अस्वस्थ होने के विषय में निर्णय करना कुछ कठिन नहीं रहता। आत्मा के स्वास्थ्य और उसके सौन्दर्य का लक्षण मन-मस्तिष्क की उदारता है। यह चीज़ अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो आपकी आत्मा निर्विकार और स्वस्थ है। अन्यथा आपकी आत्मा के अस्वस्थ होने में कोई सन्देह नहीं रहता। फिर यह अस्वस्थता मृत्यु की आहट ही सिद्ध होती है। अगर स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही दर्शाई जाए। तो इसका परिणाम विनाश और मृत्यु के सिवा कुछ और नहीं होता।
इस्लामी शिक्षाओं में इस बात पर इतना बल दिया गया है कि आश्चर्य होता है। बल इस बात पर कि आदमी दुनिया में तंगी, कठिनाई और विपत्तियों को स्वीकार कर ले किन्तु अपनी नैतिक और आध्यात्मिक मृत्यु को स्वीकार करने पर कदापि तैयार न हो। आत्मा को विनाश से बचाने के लिए किसी भी बलिदान के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक कष्ट और विपत्ति को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
कृपणता या लोभ वास्तव में मानव-आत्मा की मृत्यु है। कृपणता और लोभ वह कालकोठरी है जिसमें क़ैद होकर मानव की आत्मा घुटकर दम तोड़ देती है। आत्मा अदृश्य है। यह उसकी व्यापकता और गहनता का लक्षण है। आत्मा अदृश्य होने के बावजूद विभिन्न शैलियों में स्वयं को प्रकट करती है। इन शैलियों का सम्बन्ध मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों एवं ज्ञान और कर्म से है। भावनाओं और अनुभूतियों और कर्म के दर्पण में ही आत्मा की छवि दृश्यमान होती है। जो लोग मार्गदर्शन से वंचित होते हैं उनकी भावनाएँ और उनकी आकांक्षाएँ अत्यन्त क्षुद्र होती हैं, उनका ज्ञान पथभ्रष्ट और उनका कर्म किसी चारित्रिक उच्चता का परिचायक नहीं होता। फिर इन तीनों के बीच सन्तुलन और पूर्ण समन्वय और एकात्मता भी उनके यहाँ नहीं पाई जाती जिसके कारण उनका व्यक्तित्व वास्तविक सौन्दर्य और आकर्षण से सर्वथा वंचित होकर रह जाता है। इसके विपरीत जो लोग कृपणता और लोभ में लिप्त नहीं होते वे भली-भाँति समझ सकते हैं कि उनको हृदय और मन की जो विशालता और व्यापकता प्राप्त है वह सर्वाधिक बहुमूल्य निधि है। यही वे लोग हैं जो हिदायत (मार्गदर्शन) के सही अर्थ को समझते हैं और यही वे लोग हैं जिन्हें सही अर्थों में सत्य का आनन्द प्राप्त होता है।
अस्वाभिमान
(1) हज़रत साद-बिन-अबी वक्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अबू-बकरह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जिस किसी ने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी अन्य का बेटा कहा जबकि वह जानता हो कि वह व्यक्ति उसका बाप नहीं, उसपर जन्नत हराम है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह अत्यन्त ही निर्लज्जता और अहृदयता की बात है कि कोई जान-बूझकर स्वयं को ऐसे व्यक्ति का बेटा कहे जो वास्तव में उसका बाप नहीं है। अपने बाप का इनकार अपराध की प्रकृति की दृष्टि से कुफ़्र के सदृश है। स्वर्ग ऐसे गिरे हुए, अधम और नीच लोगों के बसने के लिए नहीं हो सकता।
इससे यह भी अन्दाज़ा किया जा सकता है कि जब अपने वास्तविक पिता को छोड़कर अपने आप को किसी दूसरे से सम्बद्ध करने के कारण आदमी स्वर्ग से वंचित हो जाता है तो ईश्वर को छोड़कर दूसरों को अपना प्रभु और पूज्य ठहराना कितना बड़ा अपराध होगा।
अकृतज्ञता
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (स्त्रियों से) कहा—
“ऐ स्त्रियों के गरोह! सदक़ा दो और अधिकाधिक क्षमा की प्रार्थना किया करो। क्योंकि मैंने देखा कि नरक में जानेवालों में तुम स्त्रियों का बाहुल्य है।" उन औरतों में से एक बुद्धिमान स्त्री ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों है कि नरक में जाने वालों में बाहुल्य हम औरतों का है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “तुम बहुत अधिक कोसती और लानत भेजती हो और पति की अकृतज्ञ होती हो। मैंने बुद्धि और धर्म में न्यून और बुद्धिमान को परास्त कर देनेवाली तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा।” वह औरत बोली कि ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी बुद्धि और धर्म में क्या कमी है? आप ने कहा, “बुद्धि की तो इससे ज़ाहिर है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होती है। यह बुद्धि की कमी हुई और औरत (महीने में) कई दिन (मासिक धर्म के दिवसों में) नमाज़ नहीं पढ़ती और रमज़ान में (मासिक धर्म के दिनों में) रोज़ा नहीं रखती, ये धर्म में कमी हुई।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : लानत भेजना और अकृतज्ञता प्रदर्शित करना ये दो ऐब ऐसे हैं जो मर्दों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। वे बात-बात पर दूसरों को कोसने और श्रापने लगती हैं। और इसी तरह साधारणतः वे अपने पतियों के उपकारों की भी उपेक्षा करती हैं और अकृतज्ञता प्रकट करती रहती हैं। ये दोनों बुराइयाँ ऐसी हैं कि उनके कारण उनका नैतिक स्तर बहुत ही गिर जाता है। और यह ऐसी ख़तरनाक परिस्थिति होती है कि अगर वे अपने आप को इस नैतिक गिरावट से बचाने और क्षतिपूर्ति की चिन्ता नहीं करतीं तो वे नरक की भागी होकर रहती हैं। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि अपनी-अपनी कमी की पूर्ति सदक़े और अधिकाधिक रूप से क्षमायाचना के द्वारा करो और प्रयास करो कि तुम इन बुराइयों से सुरक्षित रह सको।
स्त्रियों में स्मरण और बुद्धिनियोजन की कमी होती है। इसी लिए क़ुरआन में है—
“और (लेन-देन के मामले में) अपने पुरुषों में से दो गवाहों को गवाह बना लो, और यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष और दो स्त्रियाँ, जिन्हें तुम गवाह के लिए पसन्द करो, गवाह हो जाएँ। (दो स्त्रियाँ इसलिए रखी गई हैं) ताकि यदि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे।” (2 : 282)
औरत की हैसियत अबला की है। शारीरिक रूप ही से नहीं, बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से भी औरत अबला है। इसी लिए उसपर ज़्यादा बौद्धिक और वैचारिक बोझ नहीं डाला गया कि वह मर्दों की तरह दुनिया के मामलों को समझे और उनको समझाने का प्रयास करे। यह दायित्व मूलतः मर्दों का है। औरत को शारीरिक और मानसिक क्षमता प्रदान करने में यह ध्यान रखा गया है कि उसका नारीत्व शेष रहे। और यह एक तथ्य है कि स्त्री के लिए उसके अपने स्त्रीत्व से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ बहुमूल्य और सुन्दर नहीं हो सकती। अब अगर स्त्रियों में स्मरण और बुद्धिनियन्त्रण की कमी पाई जाती है तो यह कोई आपत्तिजनक विषय कदापि नहीं है। अलबत्ता यह एक तथ्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए।
औरत चाहे बुद्धि की दृष्टि से मर्द से पीछे ही क्यों न हो लेकिन उसमें कुछ ऐसा सौन्दर्य और आकर्षण पाया जाता है कि वह अपने इस जादू से बड़े से बड़े अक़्लमन्द को बेअक़्ल बना सकती है।
औरत मासिक धर्म के दिनों में नमाज़ नहीं पढ़ सकती और न ही उसके लिए उन दिनों में रोज़ा रखना जायज़ है जबकि मर्द को ऐसी कोई विवशता नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि मर्द के लिए औरत की तुलना में इबादत का अधिक अवसर उपलब्ध होता है। यह एक प्रकार की प्रमुखता (Advantage) है जो मर्दों को औरतों के मुक़ाबले में प्राप्त है। लेकिन इसके कारण औरत को कोई निकृष्ट अस्तित्व घोषित नहीं किया जा सकता। जो अन्तर भी मर्द और औरत के बीच पाया जाता है वह ईश्वर की ओर से है। धर्म की दृष्टि से पुरुष यदि स्त्री की तुलना में उच्चतर दिखाई देता है तो यह उच्चता वास्तव में केवल देखने में है। अन्यथा एक मुस्लिम महिला भी प्रत्येक हालत में ईश्वर की आज्ञाकारी और उसकी प्रसन्नता की इच्छुक होती है। अनिवार्य कार्यों के निर्वहण में पुरुष और स्त्री के मध्य जो अन्तर पाया जाता है, उसपर अगर गहराई के साथ विचार करें तो वह वास्तव में स्त्री-पुरुष का अन्तर है जो इबादतों से भी स्पष्ट है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का संकेत भी वास्तव में इसी अन्तर की ओर है।
कृपणता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"युग परस्पर (दुनिया और क़ियामत के युग) निकट होते जाएँगे और इसी के साथ कर्म में भी कमी होती चली जाएगी और कृपणता और लोभ (लोगों के दिलों में) डाला जाएगा और 'हरज' ज़्यादा होगा।” लोगों ने पूछा कि 'हरज' क्या चीज़ है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हत्या, हत्या।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक रिवायत के शब्द ये हैं—
“ज़माना परस्पर निकट होता जाएगा और ज्ञान उठा लिया जाएगा और फ़ितना प्रकट होगा और कृपणता (दिलों में) डाली जाएगी और हरज ज़्यादा होगा।"
मतलब यह है कि क़ियामत की निकटता का संकेत यह है कि लोगों में बुराइयाँ बढ़ती चली जाएँगी। ज्ञान और कर्म से लोग दूर होते जाएँगे। लोगों में लोभ, संकीर्णहृदयता और कृपणता बढ़ जाएगी। उपद्रव होगा। हत्या और रक्तपात साधारण बात होगी।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अनिवार्यतः हरेक दिन जब बन्दे सुबह करते हैं तो दो फ़रिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक कहता है कि ऐ अल्लाह, (भलाई के कामों में) ख़र्च करनेवाले को और दे, और दूसरा कहता है कि ऐ अल्लाह रोकनेवाले (कृपण) को तबाह कर।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : दानशीलता अल्लाह को इतनी प्रिय है कि फ़रिश्ता प्रार्थना करता है कि ऐ अल्लाह, इसे और दे ताकि तेरी प्रसन्नता के लिए वह अपना धन ख़र्च करता रहे। इसके विपरीत कृपणता अल्लाह को इतनी अप्रिय है कि फ़रिश्ता उससे यह प्रार्थना करता है कि अपना धन रोक रखनेवाले का धन तबाह और बरबाद कर दिया जाए कि उससे तेरे बन्दों या तेरे धर्म को किसी लाभ की आशा नहीं।
यह जो कहा गया कि प्रतिदिन जब लोग सुबह करते हैं अनिवार्यतः ये फ़रिश्ते इस तरह की प्रार्थना करते हैं। इससे मालूम हुआ कि आदमी को अपना प्रत्येक दिन दुनिया में दानशील बनकर व्यतीत करना चाहिए, न कि कृपणता, संकीर्णता और संकुचित दृष्टिकोण के साथ उसका दिन गुज़रे।
(3) हज़रत अबू-हुरैरह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
"मनुष्य में ये दुर्गुण निकृष्टतम हैं :
हद से बढ़ी हुई क्षोभपूर्ण कृपणता और लोभ, और हद से बढ़ी हुई कायरता।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : बुराइयाँ और दुर्गुण तो और भी हैं लेकिन अगर किसी के अन्दर लोभ और कृपणता और कायरता जैसा रोग पाया जाता है तो समझना चाहिए कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर (Serious) है। इसलिए कि संकीर्णहृदय और कायर व्यक्ति धर्म की बरकतों और उसके आनन्द से वंचित होता है। धर्म अगर हमारे अन्दर से कृपणता और कायरता को दूर न कर सका तो आख़िर उससे हम लाभान्वित ही क्या हुए। फिर यह बात भी है कि एक कायर, लोभी और कृपण से न ईश्वर के बन्दों को कोई लाभ पहुँच सकता है ओर न ऐसा व्यक्ति सत्यधर्म का सेवक ही हो सकता है।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"दानशील ईश्वर से निकट है, लोगों से निकट है और स्वर्ग से निकट है, और वह नरक से दूर है। जबकि कृपण अल्लाह से दूर है, लोगों से दूर है और स्वर्ग से दूर है और वह नरक से निकट है। और अवश्य ही एक दानशील अज्ञानी अल्लाह को एक इबादतगुज़ार कृपण से ज़्यादा प्रिय है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : दुनिया में सफल व्यक्ति वह है जिसे ईश्वर का सामीप्य भी प्राप्त हो और लोगों में भी वह प्रिय हो। वह स्वर्ग का पात्र हो और ईश्वर की यातना अथवा नरक से सुरक्षित हो। दानशीलता और उदारता आदमी को ईश्वर की निकटता प्रदान करती है। दानशील से लोग भी प्रेम करते हैं। अब जिस किसी को ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो और जिससे ईश्वर के बन्दों को भी कोई शिकायत न हो, उसके स्वर्ग के योग्य होने में क्या सन्देह हो सकता है। तथापि शर्त यह है कि उसके जीवन में कोई ऐसी त्रुटि न पाई जाती हो जिसके कारण आदमी के समस्त कर्म अकारथ जाते हैं। उदाहरणार्थ अधर्म, एकेश्वरवाद, कपटाचार आदि।
ईश्वर का विशेष गुण दानशीलता है। वह किसी कृपण को अपना सामीप्य कैसे प्रदान कर सकता है! कृपण अपनी कृपणता के कारण लोगों की निगाहों से भी गिर जाता है। फिर स्वर्ग को भी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं हो सकती। स्वर्ग का अधिकार तो सदाचार के द्वारा प्राप्त होता है। स्वर्ग के अधिकारी तो वही लोग हो सकते हैं जो नैतिकता के उच्च शिखर पर हों। कृपण और संकीर्णहृदय व्यक्ति तो नैतिकतारहित होता है। किसी व्यक्ति की कृपणता जिस चीज़ से उसे निकट करती है, वह है ईश्वर का क्रोध और नरक की भड़कती हुई ज्वाला।
दानशील को, यद्यपि वह विद्वान न हो, वह चीज़ प्राप्त होती है जो मूलतः जीवन में अभीष्ट है। अर्थात आत्मा की विस्तीर्णता, हार्दिक आनन्द और सुशीलता। जबकि इबादतगुज़ार कृपण इससे वंचित होता है। वह इबादतगुज़ार तो कहला सकता है लेकिन उसे चारित्रिक उच्चता प्राप्त नहीं हो सकती।
(5) हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“धोखेबाज़, कृपण और एहसान जतानेवाला स्वर्ग में प्रवेश न कर सकेगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ऐसे लोग अगर स्वर्ग में प्रवेश पा सकते तो फिर नरक को पैदा करने की आवश्यकता ही क्या थी। स्वर्ग तो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो नैतिक बुराइयों से मुक्त और चारित्रिक गुणों से सुशोभित हों।
स्वर्ग में जो सुख-सामग्रियाँ हैं और वहाँ जो आनन्द उपलब्ध है वह तो उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकता है जो उस आनन्द और सुख-सामग्रियों के पारखी और उनके आकांक्षी हों। और ये वही लोग हो सकते हैं जो स्वर्ग में प्रविष्ट होने से पूर्व अपनी शान्ति नैतिक पवित्रता और सत्कर्मों में ढूंढ़ते हैं। और इसमें सन्देह नहीं कि स्वर्ग के सुख और प्रसन्नता का प्रतिबिम्ब अगर देखा जा सकता है तो ईश्वर की याद, मन की पवित्रता और सत्कर्मों में ही देखा जा सकता है। अब अगर किसी को ईश्वर के स्मरण और सत्कर्मों में रुचि ही नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वह दुराचारी है, तो हम कह सकते हैं कि वह वास्तव में स्वर्ग का इच्छुक ही नहीं है। अब अगर किसी अनिच्छुक को स्वर्ग प्रदान कर दिया जाए तो यह स्वर्ग की गरिमा के विपरीत होगा।
क्रोध
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“पहलवान और शक्तिशाली वह नहीं जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि बलशाली वह है जो क्रोध के अवसर पर स्वयं को नियंत्रण में रखे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : आदमी को सर्वाधिक कठिनाई अपने मन को वश में रखने में पेश आती है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध में स्वयं को नियंत्रित रख सके वह वीरता में सबसे बढ़कर है।
अत्यधिक अनुचित बात पर आदमी को क्रोध आता ही है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अपेक्षित यह नहीं है कि आदमी को सिरे से क्रोध आए ही नहीं, बल्कि अपेक्षित यह है कि वह क्रोधवश ऐसे कार्य न करे जो किसी प्रकार उसे शोभा नहीं देते।
(2) हज़रत बह्ज़-बिन-हकीम (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता से और वे उनके दादा (अपने पिता) से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्रोध ईमान को भ्रष्ट कर देता है जिस तरह एलुआ शहद को भ्रष्ट कर देता है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोबिल-ईमान)
ईमान व्यक्ति में केवल विश्वास और धारणा बनकर ही नहीं रहता बल्कि ईमान के प्रभाव से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण पैदा हो जाता है। यह नैतिक गुण अपने आकर्षण और सौंदर्य में अपनी मिसाल आप होता है। अब अगर हम क्रोध पर नियन्त्रण न रख सकें तो एक मोमिन के रूप में हमारा चरित्र प्रभावित होकर रहेगा। और उसके आकर्षण और सौन्दर्य में स्पष्टतः अन्तर पैदा हो जाएगा और यह कोई साधारण हानि कदापि न होगी। जिस प्रकार एलुए की कड़ुवाहट शहद को ख़राब कर देती है उसी प्रकार क्रोध ईमान के भाव के लिए विनाशकारी होता है।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रार्थना की कि मुझे कोई वसीयत करें। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “क्रोध मत किया करो।"
उस व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना कई बार दोहराई। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हर बार यही कहा कि क्रोध मत किया करो। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक हदीस में है कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे कुछ बातों की शिक्षा दें ताकि मैं उनसे लाभ उठाऊँ। ज़्यादा बातें न बताएँ, मैं भूल जाऊँगा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्रोध मत किया करो।"
सम्भव है नबी से इस वसीयत और नसीहत की प्रार्थना करनेवाले सहाबी के स्वभाव में तनिक तीक्षणता रही हो, इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनको यह नसीहत की हो कि क्रोध मत किया करो। फिर यह भी एक तथ्य है कि जो व्यक्ति क्रोध पर नियन्त्रण रख सकेगा वह मन की दूसरी अनुचित इच्छाओं पर भी नियन्त्रण पा सकेगा। यह एक बड़ा नियम है जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें बताया।
क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। क्रोध की अवस्था में शैतान इनसान पर सरलतापूर्वक अधिकार पा लेता है और फिर उससे ऐसे-ऐसे कार्य करा जाता है कि जिनकी सामान्य परिस्थितियों में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
क्रोधावस्था में धर्म विरुद्ध बात भी लोग बक जाते हैं।
यहाँ यह बात दृष्टि में रहे कि जिस क्रोध की निंदा की गई है उससे अभिप्राय वह क्रोध है जिसके पीछे कोई तुच्छ भावना कार्यरत हो। और जिसके वशीभूत होकर इनसान ईश्वर की निर्धारित मर्यादाओं से आगे बढ़ जाता है। लेकिन वह क्रोध जो अपने लिए न हो, बल्कि जो ईश्वर के शत्रुओं के षड्यन्त्रों और उनके उठाए हुए उपद्रवों पर आ रहा हो, वह कदापि निन्दनीय नहीं है बल्कि ऐसा क्रोध तो प्रशंसनीय है। शर्त यह है कि सत्यविरोधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई भी की जाए उसमें न्याय और मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखा जा सके।
(4) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“प्रतापवान ईश्वर की दृष्टि में किसी बंदे ने क्रोध के उस घूँट से बेहतर कोई घूँट नहीं पिया जिसे वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पी जाए।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : यूँ तो जीवन में कितनी ही ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको सहन करना और पी जाना ईश्वरीय प्रसन्नता का कारण होता है लेकिन ईश्वरीय प्रसन्नता के कारण क्रोध को पीना उन सबमें श्रेष्ठ है। इसलिए कि क्रोध का घूँट पीना अत्यन्त कठिन और दुष्कर होता है। जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियन्त्रण प्राप्त हो गया समझ लीजिए कि इस एक गुण के कारण उसके लिए कितनी ही अच्छाइयों के द्वार खुलेंगे। क़ुरआन से मालूम होता है कि स्वर्ग को जिन अच्छे से अच्छे कार्य करनेवालों के लिए सुसज्जित किया गया है, उनमें जहाँ दूसरे पवित्र गुण पाए जाते हैं वहीं यह बात भी है कि "क्रोध को पी जानेवाले और लोगों के प्रति क्षमा से काम लेनेवाले हैं।” (3:134)
(5) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस किसी ने अपनी ज़बान को बन्द रखा, अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डालता है और जिस किसी ने अपने क्रोध को रोका, अल्लाह क़ियामत के दिन उससे अपनी यातना को रोक लेगा। और जो कोई उज़्र पेश करके ईश्वर से अपनी ख़ता की माफ़ी चाहता है, अल्लाह उसके उज़्र को स्वीकार कर लेता है।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
व्याख्या : ईश्वर का व्यवहार अपने बन्दों के साथ क्या होता है, यह इसपर निर्भर करता है कि स्वयं बन्दा अपने प्रभु के साथ क्या व्यवहार अपनाता है और उसका व्यवहार उसके बन्दों के साथ कैसा होता है। जो व्यक्ति दूसरों की अपने मुख से बुराई नहीं करता और न उन्हें अपमानित करता है तो ऐसे व्यक्ति की पर्दापोशी ईश्वर स्वयं करता है और उसके ऐबों को छिपाता है अन्यथा ईश्वर जिस किसी की पर्दादरी पर आ जाए, वह उसे सभी लोगों में अपमानित करके ही रहे।
इसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यन्त नागवारी महसूस करने के बावजूद लोगों पर अपना क्रोध नहीं उतारता बल्कि अपने क्रोध को पी जाता है तो ईश्वर की नीति भी उसके साथ यही होती है। वह ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध और यातना से बचाता है। इसी प्रकार यह भी असम्भव है कि कोई सच्चे दिल के साथ तौबा करे और ईश्वर से अपने पापों की क्षमा चाहे और ईश्वर उसे क्षमा न करे। ईश्वर से बढ़कर उज़्र क़बूल करनेवाला कोई अन्य नहीं हो सकता। शर्त यह है कि बन्दा सच्चे दिल से ईश्वर के समक्ष उज़्र पेश कर रहा हो और यह उज़्र पेश करना मात्र रस्म न हो।
(6) हज़रत मुआज़-बिन-अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति क्रोध को पी जाए यद्यपि उसे इसकी सामर्थ्य हो कि वह अपना क्रोध उतार सकता हो, अल्लाह उसे क़ियामत के दिन सबके सामने बुलाएगा और उसको यह अधिकार देगा कि वह स्वर्ग की मृगनयनी अप्सराओं में से जिसको चाहे अपने लिए चुन ले।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबु-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात जो व्यक्ति ऐसा नेक हो कि सामर्थ्य होने के बावजूद बदला लेने की न सोचे, बल्कि अपने क्रोध को पी जाए, तो ईश्वर की दृष्टि में उसका यह कर्म अत्यन्त प्रशंसनीय होता है। ईश्वर क़ियामत के दिन उसे जनसामान्य के समक्ष सम्मानित करेगा। दुनिया में चाहे किसी को उसकी पवित्रता और चरित्र की उच्चता का एहसास न हुआ हो लेकिन आख़िरत में ईश्वर प्रत्येक को इसका एहसास करा देगा कि वह उच्च कोटि का चरित्र रखता है। फिर वह व्यक्ति अपनी विशालहृदयता और स्वभाव की स्वच्छता का पारितोषिक सुन्दर और मृगनयनी अप्सराओं के रूप में प्राप्त करेगा।
(7) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तुममें से किसी को क्रोध आए और वह खड़ा हो तो चाहिए कि वह बैठ जाए, फिर अगर उसका क्रोध समाप्त हो जाए तो अति उत्तम अन्यथा उसे लेट जाना चाहिए।" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : क्रोध को ठंडा करने का यह एक कारगर मनोवैज्ञानिक उपाय है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बताया है। आदमी खड़ा हो तो बैठ जाए या फिर लेट जाए तो इससे अपने मन पर नियन्त्रण पाने में बड़ी आसानी होती है और इसकी सम्भावना बहुत कम बाक़ी रहती है कि वह ऐसी अनुचित और व्यर्थ की हरकतें करे जैसी हरकतें साधारणतः लोग क्रोध में आकर कर बैठते हैं।
(8) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"लोगों को शिक्षा दो, और आसानी पैदा करो, कठिनाई पैदा न करो, और जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले। जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले। जब तुममें से किसी को क्रोध आ जाए तो उसे चाहिए कि मौन धारण कर ले।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अत-तबरानी-फिल-कबीर)
व्याख्या : इस हदीस से कई बातें मालूम हुईं। लोगों को धर्म की शिक्षा से अवगत कराना आवश्यक है। तंगी और कठिनाई की जगह आसानी और सुविधा पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। और अगर किसी बात पर क्रोध आ जाए तो आदमी को मौन रहने का फ़ैसला कर लेना चाहिए। एक मौन हज़ार मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। इसको न भूलना चाहिए। मौन धारण कर लेने से बात के आगे बढ़ने की सम्भावना शेष नहीं रहती। अन्यथा क्रोध में बात बढ़ते-बढ़ते अकसर हाथापाई तक की नौबत आ जाती है जो किसी प्रकार मोमिन को शोभा नहीं देता।
(9) हज़रत अतिया-बिन-उरवा सादी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्रोध शैतान के प्रभाव से आता है और शौतान आग से पैदा किया गया है। और आग केवल पानी से बुझती है। अतः जब तुम में से किसी को क्रोध आए तो उसे चाहिए कि वुज़ू कर ले।" (हदीस : अबू दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस में भी क्रोध का एक इलाज प्रस्तावित किया गया है। वह यह कि अगर किसी को क्रोध आ जाए तो वह वुज़ू कर ले। इससे उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। बताया गया कि क्रोध (साधारणतः) शैतान के प्रभाव से आता है, और शैतान अग्नि का स्वभाव रखता है। जिस प्रकार आग को पानी से बुझाते हैं उसी प्रकार शैतान के प्रभाव को दूर करने के लिए भी पानी का प्रयोग करना चाहिए। क्रोध आ जाए और उसे आदमी नियन्त्रित नहीं कर पा रहा हो तो वह उठकर वुज़ू कर ले। (यानी हाथ-पैर धो ले)
अतिवादिता और कठोर स्वभाव
(1) हज़रत हारिसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“स्वर्ग में उजड्ड, कठोर एवं उग्रभाषी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।” (हदीस : शरहस्सुन्नह)
व्याख्या : उजड्ड के लिए मूल में ‘जव्वाज़’ शब्द आया है। जव्वाज़ के अर्थ कई विद्वानों ने अहंकारी के भी लिए हैं। यह भी कहा गया है कि जव्वाज़ वह व्यक्ति है जो माल जमा करे और माँगनेवाले को न दे।
कठोरता या उग्रता चाहे स्वभाव में हो या नीति में, यह अत्यन्त अप्रिय है। अप्रिय और बुरी चीज़ का स्वर्ग से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।
इस्लाम दिलों को शान्ति और आत्मा को चैन प्रदान करने आया है। वह मन-मस्तिष्क को उदारता और हृदय को जीवन्तता प्रदान करता है। वह बेहौसला लोगों को हौसला देता है। वह टूटे हुए दिलों के लिए आशा बनकर प्रकट हुआ है। वह लोगों को उनके कल्याण और सफलता के रास्ते पर लगाना चाहता है। इस्लाम जिसका पैग़ाम मुहब्बत हो, जो एकता, सहयोग, समानता और न्याय की शिक्षा देता हो, जिसमें इतनी व्यापकता हो कि सम्पूर्ण मानवता को एक कुटुम्ब क़रार देता हो, क्षमा से काम लेने का आदेश देता हो। 'कूनू इबादल्लाहि इख़्वाना' (अर्थात ईश्वर के बन्दे और भाई-भाई बनकर रहो) जिसकी माँग हो वह कठोरता और उग्रता को कैसे पसन्द कर सकता है। अनुचित कठोरता किसी भी मामले में उसे पसन्द नहीं। कठोरता और अतिवादिता न धर्म के मामले में सही है और न सांसारिक मामलों में सही हो सकती है। वे लोग इस्लाम की प्रकृति से नितान्त अपरिचित हैं जो छोटी-छोटी बातों को लेकर तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। इस्लाम जिस सभ्यता एवं जिस कर्म और चिन्तन-प्रणाली का ध्वजावाहक है उसका प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता जो बुरे स्वभाव का और पाषाण-हृदय हो। फिर जिसे न तो इस्लाम के प्रतिनिधित्व की चिन्ता है और न उसे व्यक्तिगत हैसियत से इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में अपने व्यक्तित्व के निर्माण की चिन्ता है, उसे आख़िर किस प्रकार यह शुभ सन्देश दिया जाए कि तुम चाहे जैसे हो तुम्हारे लिए स्वर्ग में उच्च कोटि के आवास का आवंटन हो चुका है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे वर्णन करते हैं कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। लोग उसपर बिगड़ने लगे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर एक बड़ा डोल पानी बहा दो। तुम तो आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, सख़्ती के लिए तुम्हें नहीं भेजा गया है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इस हदीस से भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि इस्लाम में धैर्य, सहनशीलता और क्षमा से काम लेने का कितना महत्व है। उत्तेजना या अनुचित कठोरता और अतिवादिता मोमिन की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा के कदापि अनुकूल नहीं हो सकती।
कठोर-हृदयता
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ईश-स्मरण के बिना बहुत बातें न किया करो क्योंकि बिना ईश्वर के स्मरण के बहुभाषिता हृदय की कठोरता का कारण होती है। और याद रखो, लोगों में ईश्वर से सबसे अधिक दूर वह व्यक्ति होता है जो हृदय का कठोर हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि आदमी के जीवन की सफलता का असली रहस्य यह है कि वह हमेशा ईश्वर से निकट रहे। ईश्वर का स्मरण और उसकी याद ही आदमी को ईश्वर से निकट रखती है। यह स्मरण ही हृदय का आहार है। यही हृदय को नर्म रखता है। नर्मी और द्रवशीलता ही वास्तव में हृदय है। अगर हृदय में नर्मी शेष न रहे तो वास्तव में वह हृदय ही नहीं रहता। हृदय का अभाव मनुष्य को ईश्वर से भी वंचित कर देता है। इसलिए कि हृदय ही वह वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य का अपने प्रभु से सम्बन्ध स्थापित होता है।
यह हदीस यह भी बताती है कि अधिक बोलना हृदय की कठोरता और निर्ममता का कारण बनता है। बहुत अधिक बोलनेवाला साधारणतः अपनी ही बात की धुन में रहता है। उसे दूसरों की बातों की बहुत ही कम परवाह होती है, चाहे दूसरे की बात सत्य ही क्यों न हो। फिर ऐसा व्यक्ति लोगों से घाल-मेल का अधिक इच्छुक रहता है ताकि उसे अपनी बात का सिक्का जमाने का अवसर मिल सके। यह चीज़ उसे इस बात से बेपरवाह रखती है कि उसे जीवन में मूलतः किस बात की चिन्ता होनी चाहिए और वस्तुतः वह कौन-सी चीज़ है जिसे ईश्वर ने मनुष्यों के लिए सही अर्थों में शान्ति और सन्तोष का निमित्त बनाया है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अपने हृदय की कठोरता की शिकायत की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अनाथ के सिर पर हाथ फेरा करो और दरिद्र को खाना खिलाया करो।” (हदीस : अहमद)
व्याख्या : इससे पहले जो हदीस गुज़र चुकी है उसमें हृदय के स्वास्थ्य और उसकी जीवन्तता के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि आदमी ईश्वर के स्मरण और उसकी याद से कभी ग़ाफ़िल न रहे। इस हदीस में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कठोर हृदयता का एक उपचार प्रस्तावित किया है। और वह यह कि आदमी अनाथों के सिर पर हाथ फेरे और मुहताजों और भूखों को खाना खिलाए। यह इलाज मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है। जिन लोगों के दिलों में विनम्रता या दया की भावना पाई जाती है वे भूखों और दरिद्रों को देख तड़प उठते हैं। वे उन भूखों को खिलाने की चिन्ता करते हैं। इसी प्रकार अनाथों पर भी उन्हें दया आती है और वे उनके सिर पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरते हैं ताकि उन्हें अपनी बेचारगी का एहसास न सताए और वे यह समझ सकें कि दुनिया में उनसे भी प्यार और मुहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। अब ऐसे विनम्र और दयालु लोगों की नीति अपनाने से अनिवार्यतः कठोर हृदय व्यक्ति के हृदय में भी दयाभाव जागृत होता है और शनैः शनैः उसके हृदय की कठोरता दूर हो सकती है।
इसके अतिरिक्त अनाथ मृत्यु की याद दिलाता है। हम जानते हैं कि मृत्यु ही ने उससे उसके माता-पिता को विलग किया है। मृत्यु का विचार आते ही हृदय नर्म पड़ जाता है। दरिद्र को खाना खिलाना आदमी को ईश्वर के उस उपकार की याद दिलाता है जो ईश्वर ने उसे सुखी-सम्पन्न बनाकर उसपर किया है। स्पष्ट है कि इस सूरत में भी आदमी के हृदय की दशा वह नहीं रहती जो एक कठोरहृदय व्यक्ति के हृदय की होती है।
द्वेष और शत्रुता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। और न तो लोगों की बातों की टोह में रहो और न एक-दूसरे के शत्रु बनो। बल्कि एक-दूसरे के भाई बने रहो। और कोई व्यक्ति अपने भाई की मँगनी पर मँगनी का पैग़ाम न भेजे यहाँ तक कि वह निकाह कर ले या फिर मँगनी छोड़ दे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि ईमानवालों के पारस्परिक सम्बन्ध कितने प्रीतिकर होने चाहिएँ। इस्लाम जिस आदर्श समाज के निर्माण की माँग करता है उसके लिए अपरिहार्य है कि समाज के व्यक्तियों के दिल एक-दूसरे की ओर से बिल्कुल साफ़ हों। उनमें एक-दूसरे के लिए शत्रुता या घृणाभाव कदापि न पाया जाए। वे एक-दूसरे की कमज़ोरियों की तलाश में हरगिज़ न रहें बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई की मान-मर्यादा का रक्षक हो। वे कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी दूसरे का दिल टूटे और जो सहानुभूति और हितचिन्ता के विरुद्ध हो। उदाहरण स्वरूप अगर किसी ने किसी के यहाँ शादी का पैग़ाम भेजा है तो फिर यह किसी प्रकार उचित न होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पैग़ाम के बाद वहाँ अपना पैग़ाम भेजे। हाँ, अगर लड़कीवाले उस पैग़ाम को स्वीकार न करें या किसी कारणवश मँगनी का पैग़ाम भेजने वाला स्वयं ही अपने पैग़ाम को वापस ले ले तो फिर दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह वहाँ शादी के लिए अपना पैग़ाम भेजे।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। और न तो लोगों की बुराइयों की टोह में रहो और न खोज में और न (दुनिया का) लोभ करो और न इर्ष्या करो। और न द्वेष रखो और न एक-दूसरे से पीठ फेरो बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई-भाई बनकर रहो।” (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : इस हदीस में भी इस उपाय की चर्चा की गई है कि किस प्रकार इस्लामी समाज की पवित्रता को बाक़ी रखा जाए। साधारणतः दुनिया का लोभ मनुष्य को अन्याय और अत्याचार पर उभारता है और वह उस विशालहृदयता और उच्चता का प्रदर्शन नहीं कर पाता जो इस्लाम में अभीष्ट है। इसलिए इसमें दुनिया के लोभ-लालच से दूर रहने की ताकीद की गई है।
इस हदीस में अत्यन्त संक्षिप्त और संग्राहक शब्दों में इस्लामी समाज की वास्तविक विशेषता का वर्णन किया गया है जो इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ईश्वर की ओर से 'जवामिउल कलिम' प्रदान किया गया था। अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह योग्यता प्राप्त हुई थी कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के संक्षिप्त शब्दों में अर्थों का बाहुल्य पाया जाता था। आप कहते हैं, "कूनू इबादल्लाहि इख़वाना।" (अल्लाह के बन्दे और भाई-भाई बनकर रहो।) कितने सुन्दर और प्रभावी शब्दों में ईमानवालों का सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है। मोमिन ईश्वर के द्रोही नहीं बल्कि उसके आज्ञाकारी बन्दे होते हैं और वे परस्पर एक-दूसरे के शत्रु नहीं बल्कि भाई बनकर रहते हैं। ऐसे भाई जो एक-दूसरे के शुभ-चिन्तक और दुख दूर करनेवाले होते हैं।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सोमवार और गुरुवार के दिन स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। और हर ऐसे बन्दे को क्षमा कर दिया जाता है जो ईश्वर के साथ किसी को साझी न ठहराता हो। अलबत्ता वह व्यक्ति क्षमा से वंचित रह जाता है जिसकी अपने और अपने किसी भाई के मध्य शत्रुता हो। इस दशा में (फ़रिश्तों) से कहा जाता है कि इन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को फ़रिश्तों के बीच इसकी पुष्टि और इसका प्रदर्शन किया जाता है कि वे लोग जो ईश्वर के साथ किसी को साझी नहीं ठहराते और न उन्हें अपने भाइयों से कोई द्वेष और शत्रुता है, उन्हें क्षमा कर दिया गया। वही ईश्वर के स्वर्ग के वारिस हैं। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। मानो स्वर्ग को अब अपने वासियों के अतिरिक्त किसी और चीज़ की प्रतीक्षा नहीं। इसे सप्ताह में दो बार दोहराया जाता है। और उन स्वर्गवालों को याद किया जाता है जो अभी दुनिया ही में होते हैं, अभी वे दुनिया से वापस नहीं हुए होते।
लेकिन इस अवसर पर उन लोगों के क्षमादान की घोषणा नहीं की जाती जिनके सम्बन्ध परस्पर सुधरे हुए न हों। जो अपने भाई से कपट और द्वेष रखते हों। उनका मामला स्थगित कर दिया जाता है। उनका क्षमादान, पारस्परिक सुलह और द्वेष मिट जाने पर निर्भर करता है। इससे मालूम हुआ कि ईश्वर और उसके बन्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक रहने ही पर यह निर्भर करता है कि हमें क्षमा कर दिया जाए और हम मुक्ति के अधिकारी हो सकें। बल्कि पारस्परिक सम्बन्धों का ठीक रहना ही हमारी मुक्ति है। मुक्ति और पारस्परिक सम्बन्धों की मधुरता के मध्य अत्यन्त गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। और यह सम्बन्ध बीज और वृक्ष के आपसी सम्बन्ध से भी अधिक निकट का होता है।
कायरता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“आदमी में सबसे बुरी बात ग़म में डालने और कुढ़न पैदा करनेवाला लोभ और घबरा देनेवाली कायरता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : लोभी और कृपण व्यक्ति हमेशा इस दुख में पड़ा रहता है कि उसे अमुक-अमुक वस्तु प्राप्त नहीं और अमुक व्यक्ति धन-सम्पत्ति में मुझसे बहुत आगे है। इसी प्रकार कायर व्यक्ति भी हमेशा कल्पित ख़तरों से घबराता रहता है। वह कभी चैन की साँस नहीं ले सकता। हृदय की ये दोनों ही अवस्थाएँ अत्यन्त निकृष्टतम अवस्थाएँ हैं। इसलिए कि इनके कारण आदमी ईश्वरप्रदत्त जीवन से सही फ़ायदा उठाने में असमर्थ रहता है। उसके हृदय में कभी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सुख-शान्ति जीवन की सबसे बड़ी निधि है। जो वस्तु मनुष्य से उसका सुख-चैन छीन ले उसके लिए उससे बुरी वस्तु क्या होगी।
हम कायरता, लोभ और कृपणता से अपने हृदय को सदैव मुक्त रखने का प्रयास करें। यही इस हदीस की मूल शिक्षा है।
साहसहीनता
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुममें से कोई (शारीरिक या धन-सम्बन्धी) कष्ट और हानि के कारण जो उसे पहुँचे, मृत्यु की कामना न करे। और अगर इस प्रकार की कामना करनी उसके लिए अपरिहार्य हो जाए तो उसे यह कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे उस समय तक जीवित रख जब तक जीवन मेरे लिए अच्छा हो और उस समय मृत्यु दे जबकि मेरा मरना अच्छा हो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : जीवन जैसी बहुमूल्य निधि समाप्त होने की कामना कृतघ्नता है। इसलिए इस्लाम ने आत्महत्या तो दूर मृत्यु की कामना करने से भी रोका है। साधारणतः लोग विपत्तियों या आज़माइशों में हिम्मत हार जाते हैं और वे मौत के दामन में पनाह ढूँढते हैं। यह मोमिन की गरिमा के प्रतिकूल है। अलबत्ता ईश्वरीय मार्ग में शहीद होने की आकांक्षा दूसरी चीज़ है। अतएव मुस्लिम की एक हदीस में है कि जिस व्यक्ति ने सच्चे दिल से और शुद्ध हृदय से शहीद होने की कामना की उसे शहादत का प्रतिदान प्राप्त होता है (चाहे उसकी मृत्यु बिस्तर पर ही क्यों न हुई हो)।
इमाम नव्वी की दृष्टि में अपने धर्म के फ़ितने में पड़ने और उसके विकृत होने के भय से मृत्यु की कामना करना बुरा नहीं, बल्कि वे इसे उचित समझते हैं।
अनुचित उदारता
(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मक़ाम और मर्तबे की दृष्टि से निकृष्टतम व्यक्ति ईश्वर की निगाह में क़ियामत के दिन वह होगा जिसने दूसरे की दुनिया बनाने में अपनी आख़िरत बरबाद कर दी।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : स्वयं अपने सांसारिक लाभ को पारलौकिक लाभ पर प्राथमिकता देना बड़े घाटे की बात है। इससे बढ़कर घाटे की बात यह होगी कि कोई दूसरों को प्रसन्न करने और उनको सांसारिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से स्वयं अपने परलोक को तबाह करले। वह अगर दूसरों को सांसारिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उचित-अनुचित और हलाल और हराम में अन्तर नहीं करता तो उससे बढ़कर बुद्धिहीन और अदूरदर्शी दूसरा कौन हो सकता है! ऐसा व्यक्ति ईश्वर की पकड़ और परलोक की यातना से बच नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति अनिवार्यतः निकृष्टतम और अत्यन्त ही बुरा आदमी समझा जाएगा जिसने न तो सत्य का कुछ ध्यान रखा और न ईश्वर की प्रदान की हुई बुद्धि से कुछ काम लिया।
अनुचित भाव ग्रहण करना
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जो व्यक्ति (वेश-भूषा आदि में) किसी क़ौम के सदृश बने तो वह उसी क़ौम का है।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिए यह वैध न होगा कि वे किसी क़ौम से इतने प्रभावित हो जाएँ कि बिल्कुल उसी क़ौम के लोगों का रहन-सहन, परिधान, रख-रखाव, विचारशैली, आचार-व्यवहार आदि अपना लें कि उनकी अपनी मौलिकता और विशिष्टता शेष न रहे। ग़ैर-मुस्लिमों के विशिष्ट रंग-ढंग को अपनाने का अर्थ यह होता है कि हमें अपनी धार्मिक स्मिता और इस्लामी सभ्यता का कुछ ध्यान नहीं रहा। हम दूसरों की सभ्यता, दूसरों की संस्कृति और उनके रीति-रिवाजों को दिल से पसन्द करते हैं। आदमी की पहचान उसकी पसन्द और नापसन्द और उसकी अभिरुचि से ही होती है। ग़ैरों के रंग-ढंग और उनकी अपनी विशिष्ट चीज़ों को अपनाकर आदमी इस बात का प्रमाण देता है कि वह अपनी अभिरुचियों और भावनाओं की दृष्टि से उन ही के साथ है, और यह इस्लामी चरित्र के लिए किसी मृत्यु से कम नहीं।
यहाँ यह तथ्य दृष्टि में रहे कि किसी क़ौम की कोई लाभप्रद वस्तु लेना इस हदीस के प्रतिकूल नहीं है। ख़राबी उस समय पैदा होती है जब कोई व्यक्ति ग़ैर-क़ौम की सभ्यता और नैतिकता और उसके रहन-सहन का ऐसा अन्धानुकरण करने लग जाए कि उसे इसकी कोई परवाह ही न हो कि इससे उसकी सामुदायिक विशिष्टता और गरिमा शेष भी रह सकती है या नहीं।
पक्षपात
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति नाहक़ अपनी क़ौम का समर्थन करे वह ऐसा ही है जैसे कोई ऊँट कुँए में गिर पड़े, फिर उसे उसकी दुम पकड़ कर खींचा जाए।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अपनी क़ौम के लोग अगर असत्य के लिए लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई में उनका साथ मात्र इसलिए देना कि वे अपनी क़ौम के हैं, जाहिली पक्षपात है। इस्लाम का इससे दूर का भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो कोई सत्य को छोड़ कर अन्याय और अत्याचार की नीति अपनाता है, वह वास्तव में स्वयं को तबाह और बरबाद करता है। उसकी इस नीति से उसका धर्म और चरित्र भ्रष्ट होकर रह जाता है। उसकी दशा उस ऊँट की सी होती है जो किसी कुँए में गिर पड़ा हो। कुँए में गिरे हुए ऊँट को उसकी दुम पकड़कर नहीं निकाला जा सकता। अत्याचारी का समर्थन और उसकी सहायता उसे उस तबाही से नहीं बचा सकती जिसको उसने स्वयं ही अपने लिए पसन्द कर लिया है। अपनी क़ौम का समर्थन करना और उसे बचाना तो दूर, वह तो स्वयं जाहिली पक्षपात के कारण तबाह और हलाक होता है। फिर उसका कोई धार्मिक और नैतिक महत्व शेष नहीं रहता।
धिक्कार और भर्त्सना
(1) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि—
“लानत करनेवाले न गवाह होंगे और न सिफ़ारिश कर सकेंगे।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात उन्हें क़ियामत के दिन यह दर्जा न प्राप्त हो सकेगा कि उनकी गवाही को महत्व दिया जाए और न उन्हें किसी के पक्ष में सिफ़ारिश करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। बहुत अधिक लानत-मलामत करनेवाले लोग साधारणतः वही होते हैं जो संकीर्णहृदय और संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अन्दर न ज्ञान होता है और न सहनशीलता होती है और न उनमें विचार और चिन्तन की कोई क्षमता होती है। हालात के अच्छे-बुरे प्रभाव और इनसान की मजबूरियों और उसकी मानसिक कठिनाइयों की वे कुछ भी ख़बर नहीं रखते। कोई बात उन्हें नागवार महसूस हुई नहीं कि वे लगे धिक्कारने। ऐसा नहीं होता कि उन्हें लोगों के सुधार की चिन्ता हो और सुधारकार्य में उनका कोई बड़ा योगदान हो। ऐसे लोग ईश्वर की दृष्टि में कभी विश्वासपात्र नहीं हो सकते।
दुष्चरित्रता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन ईश्वर की दृष्टि में लोगों में सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा जिसकी असभ्यता के कारण लोग उससे मिलना छोड़ दें।" (हदीस : अबु-दाऊद)
व्याख्या : यह बात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक विशेष अवसर पर कही थी। एक बार एक व्यक्ति ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मुलाक़ात की आज्ञा चाही, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि "यह कुटुम्ब का बुरा आदमी है।" फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे अन्दर आने की अनुमति दी और उससे अत्यन्त नर्मी से बात की। हज़रत आयशा ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि आपने तो उससे बड़ी नर्मी से बातें कीं हालाँकि आप कह चुके हैं कि वह कैसा है! इस मौक़े पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वह बात कही जो यहाँ उद्धृत की गई है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कहने का अर्थ यह है कि आदमी को कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर किसी बुरे व्यक्ति से पाला पड़ जाए फिर भी आदमी को अपनी सज्जनता को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
अध्याय-4
सामाजिक विकृतियाँ
(1)
अन्तर्दृष्टि का अभाव
कपटाचार
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कपटी के तीन लक्षण हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादाख़िलाफ़ी करे और जब उसे विश्वासपात्र और भरोसे के योग्य समझा जाए तो वह विश्वासघाती निकले।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : कपटाचार यह है कि आदमी दावा तो अपने मोमिन और मुस्लिम होने का करे मगर वस्तुतः उसका दिल ईमान से रहित हो। कपटाचार वास्तव में चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। इसलिए उसे कुफ़्र से भी बढ़कर घृणायोग्य समझा गया है। क़ुरआन में है—
“कपटाचारी आग (नरक) के सबसे निचले खंड में होंगे, और तुम कदापि उनका कोई सहायक न पाओगे।” (4:145)
इस हदीस से मालूम होता है कि यह नीति कपटाचारी की होती है कि वह झूठ बोले और अपने दिए हुए वचन का वह कोई आदर न करे लेकिन यहाँ यह भी दृष्टि में रहे कि झूठ और वचनभंग और इस प्रकार के दूसरे कपटपूर्ण दुर्गुण कोई अपनाता है तो इसकी सम्भावना है कि यह व्यावहारिक कपटता उस व्यक्ति को वास्तविक कपटाचार में लिप्त कर दे। क़ुरआन में है—
“फिर परिणाम यह हुआ कि उसने उनके दिलों में उस दिन तक के लिए कपटाचार डाल दिया जब वे उससे मिलेंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो प्रतिज्ञा की थी उसे भंग कर दिया और इसलिए भी कि वे झूठ बोलते रहे।” (9:77)
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस व्यक्ति में ये चार बातें पाई जाएँ वह पूरा कपटाचारी है और जिस किसी में इनमें से कोई एक लक्षण हो उसमें कपटाचार का एक लक्षण पाया जाता है यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे : जब उसे विश्वासपात्र समझा जाए तो वह विश्वासघाती सिद्ध हो, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वचन दे तो उसे भंग कर दे और जब झगड़ा करे तो बेक़ाबू हो जाए।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : सही मुस्लिम में यह भी है कि—
“यद्यपि वह रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े और इसका दावा करे कि वह मुस्लिम है।"
अर्थात नमाज़-रोज़ा आदि जैसी इबादतों से किसी को धोखा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के अन्दर चरित्र का यह अवगुण पाया जाता है तो उसकी नमाज़ और रोज़े को देख कर वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। जीवन के आन्तरिक और बाह्य जीवन का यह अन्तर्विरोध, धोखाधड़ी और फ़रेबकारी वास्तव में कपटाचार ही है। इस हदीस में जिन अवगुणों का उल्लेख किया गया है उन सबके पीछे मूलतः फ़रेबकारी का अवगुण ही कार्यरत है। फ़रेबकारी के यूँ तो बहुत-से रूप हो सकते हैं। यहाँ जिन पाँच चीज़ों का उल्लेख किया गया है उनकी हैसियत बुनियादी है। समाज में हमें बहुधा इनका सामना करना पड़ता है। विश्वासघात, स्वार्थपरता, वचनभंग आदि लक्षणों का उल्लेख क़ुरआन में अत्यन्त विस्तार से किया गया है।
(3) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कपटाचारी की मिसाल उस परेशान बकरी की-सी है जो दो रेवड़ों के बीच कभी इस ओर कभी उस ओर मारी-मारी फिरती हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : कपटाचार अत्यन्त निकृष्टतम नीति है। इसका एहसास दिलाने के लिए इस हदीस में कपटाचारी की मिसाल उस आवारा बकरी से दी गई है जो नर की तलाश में इधर-उधर मारी फिरती है। कपटाचारियों के कायर गरोह की हालत इससे भिन्न नहीं होती। कपटाचारियों को केवल अपने सांसारिक हित प्रिय होते हैं। सांसारिक हितों के तहत ये कभी मुसलमानों से अपनी अनुचित आस लगाते हैं तो कभी अधर्मियों के पास दौड़े जाते हैं। परिस्थितियों का मुक़ाबला वीरतापूर्वक स्वयं करें, इसकी सामर्थ्य कपटाचार का रोग उनके अन्दर शेष नहीं रहने देता।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति इस हाल में मरा कि न तो उसने (ईश्वरीय मार्ग में) कभी युद्ध किया और न उसके दिल में इसका ख़याल गुज़रा तो उसकी मृत्यु कपटाचार की एक शाखा के अन्तर्गत हुई।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : कपटाचारी हमेशा युद्ध से जी चुराते रहे हैं। जबकि मोमिन की अस्ल शान यह होती है कि वह ईश्वरीय मार्ग में अपने प्राण न्योछावर करने का अभिलाषी होता है। उसकी यह आकांक्षा कि काश वह ईश्वरीय मार्ग में क़ुरबान हो! इस बात का प्रमाण है कि उसे ईश्वर और उसके रसूल से प्रगाढ़ प्रेम है। कोई दूसरी चीज़ उस प्रेम पर वर्चस्व नहीं प्राप्त कर सकती।
ईश्वरीय मार्ग में जान देने का अवसर न भी आए लेकिन मोमिन का हृदय इस भावना से कभी रिक्त नहीं होता कि उसकी जान ईश्वर के लिए क़ुरबान हो और उसका रक्त ईश्वरीय मार्ग में बहे।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह दुआ करते थे—
अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ु बि-क मि-नश-शिक़ाक़ि वन-निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़।
ऐ अल्लाह, मैं (सत्य से) विरोध, कपटाचार और दुराचार से सुरक्षित रहने के लिए तेरी शरण लेता हूँ।" (हदीस : अबू-दाऊद, नसई)
व्याख्या : यह एक संग्राहक प्रार्थना है। इससे अनुमान होता है कि आदमी को कपटाचार से कितना बचना चाहिए।
विरोध और दुश्मनी के लिए मूल में 'शिक़ाक़' शब्द प्रयुक्त हुआ है। शिक़ाक़ और दुराचार का कपटाचार से गहरा सम्बन्ध होता है। बल्कि यह वास्तव में कपटाचार ही की अपेक्षाओं में से है। कपटाचारी चरित्रवान और वास्तविक मित्र हो ही नहीं सकता। कपटाचार चरित्र की मृत्यु है। कपटाचारी मानव समाज में सर्वाधिक कुरूप और निकृष्टतम अस्तित्व होता है। हमारे लिए आवश्यक है कि कपटाचार और उसकी बुराइयों से पूर्णतः अवगत रहें और उनसे सुरक्षित रहने के लिए ईश्वर का आश्रय लेते रहें।
स्वार्थपरता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कोई व्यक्ति अपने (मुसलमान) भाई के वैवाहिक प्रस्ताव पर अपना प्रस्ताव न भेजे यहाँ तक कि वह विवाह कर ले या उससे अपना हाथ खींच ले।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अगर कहीं किसी व्यक्ति ने अपना वैवाहिक प्रस्ताव भेजा है और इस सम्बन्ध में उसकी बात-चीत चल रही है तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह पूर्णतः वर्जित है कि वह उसी जगह अपना वैवाहिक प्रस्ताव भेजे। हाँ अगर किसी कारणवश जो बातचीत प्रारम्भ हुई थी, समाप्त हो जाती है और रिश्ता तय नहीं होता तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं रह जाता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी जगह अपने या किसी अन्य के लिए बातचीत प्रारम्भ करे।
शादी और विवाह ही नहीं, क्रय-विक्रय, लेन-देन और दूसरे मामलों में भी शरीअत ने ऐसी ही पाबन्दी लगाई है। यह तो ओछेपन और स्वार्थपरता की बात होगी कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को ख़रीदना चाहता है और वह उसके लिए उसके मालिक से बातचीत कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ का ख़रीदार बनकर खड़ा हो जाए। जब तक पहला व्यक्ति सौदे से हाथ नहीं खींच लेता, किसी दूसरे के लिए यह वैध नहीं है कि वह उसे ख़रीदने का प्रयास करे।
इसी प्रकार अगर किसी रिक्शे या अन्य सवारी वाले से कोई व्यक्ति कहीं ले चलने के लिए बात कर रहा हो तो यह उचित न होगा कि उसकी उस बातचीत के बीच ही में कोई दूसरा व्यक्ति आकर रिक्शे या अन्य सवारी वाले से अपने लिए बात करने लग जाए या आकर सवार हो जाए और कहे कि मुझे अमुक स्थान तक ले चलो। अलबत्ता अगर पहले व्यक्ति का मामला तय नहीं होता और वह हट जाता है तो अब दूसरे व्यक्ति के लिए इसका पूरा अवसर है कि वह बात-चीत करके मामला तय करे।
अनुत्तरदायी नीति
(1) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता से और वे अपने दादा से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो कोई चिकित्सक बन बैठे हालाँकि उसके चिकित्सक होने का प्रमाण न हो तो वह (रोगी की मृत्यु या उसके रोग के बढ़ जाने का) ज़िम्मेदार होगा।" (हदीस : अबू-दाऊद, नसई)
व्याख्या : जिसको चिकित्साशास्त्र का ज्ञान और अनुभव न हो और वह चिकित्सक बन बैठे, लोगों का इलाज करने लग जाए तो वह रोगी पर अत्याचार करेगा।
बिना ज्ञान और अनुभव के अगर वह लोगों का इलाज करता है तो इसका मतलब इसके सिवा और क्या होगा कि वह लोगों की जानों से खेल रहा है। सरकार ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देने का अधिकार रखती है। ऐसा नक़ली चिकित्सक अगर किसी रोगी का इलाज करे और रोगी मर जाए तो वह नक़ली चिकित्सक उत्तरदायी है। दियत (दंड-धन) उसपर वाजिब होगी। यह हदीस बताती है कि आदमी को जीवन में अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए यह किसी हालत में भी उचित नहीं हो सकता कि वह किसी मामले में केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने रखे और अनुत्तरदायित्वपूर्ण नीति अपनाए।
दोरुख़ापन
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन तुम निकृष्टतम व्यक्ति उसको पाओगे जो दो मुँह रखता है। इन लागों के पास एक मुँह लेकर आता है और उन लोगों के पास दूसरा मुँह लेकर जाता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मुस्लिम की एक हदीस में यह आया है—
“निश्चय ही निकृष्टतम व्यक्ति वह है जो दो मुँह रखता हो। इन लोगों के पास आता हो तो एक मुँह लेकर और उन लोगों के पास जाता हो तो दूसरा मुँह लेकर।"
यह सत्यवादिता और दयानतदारी के प्रतिकूल है कि आदमी सत्य-असत्य को भुला दे और जिस किसी के पास जाए बस उसी की-सी बात करने लगे। यह एक प्रकार का कपट और अवसरवादिता है जिसको हमेशा बुरा समझा गया है। ऐसा आदमी ख़ुशामदी होता है और बहुत जल्द वह अपना विश्वास खो देता है। फिर किसी को उसपर भरोसा नहीं होता।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर दो गरोहों में या दो आदमियों में कोई झगड़ा और कोई मतभेद पाया जाता है तो वे दोनों में से हरेक से अपना विशेष लगाव प्रकट करेंगे और जब एक पक्ष के यहाँ पहुँचेंगे तो दूसरे को बुरा कहेंगे। इस कोटि के व्यक्ति को अरबी में 'ज़ुल-वजहैन’ अर्थात दोमुँहा कहते हैं।
(2) हज़रत अम्मार (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जो व्यक्ति दुनिया में दो मुँह रखता होगा क़ियामत के दिन उसके मुँह में आग की दो ज़बानें होंगी।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इमाम ग़ज़ाली ने दोतरफ़ा बातें बनाने को चुग़लख़ोरी के दुर्गुण से भी अधिक बुरा ठहराया है। चुग़ली में आदमी केवल एक की बात दूसरे के यहाँ पहुँचाता है और यहाँ दोतरफ़ा विरोधी बातें पहुँचाई जाती हैं या दोनों पक्षों में से हरेक के यहाँ जाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास किया जाता है। हरेक पक्ष से सिर्फ़ उसी की सी बात कही जाती है और उसके प्रति अपने समर्थन का विश्वास दिलाया जाता है। जिस व्यक्ति का यह स्वभाव होगा उसे 'ज़ुल-वजहैन' और ‘ज़ुल्लिसानैन' (दो चेहरों और दो ज़बानों वाला) कहा जाएगा। क़ियामत में उसको आग की दो ज़बानें दी जाएँगी। यह दंड उसके अपने कृत्य के सर्वथा अनुकूल होगा।
(2)
कुरुचि
बदगुमानी
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सर्वाधिक झूठी बात है। किसी की भलाई-बुराई से अवगत होने का प्रयास न करो, न टोह में पड़ो, न दूसरे से बढ़कर बोली बोलो, न परस्पर ईर्ष्या करो, न आपस में द्वेष रखो, न परस्पर शत्रुता या सम्बन्ध विच्छेद करो, और ईश्वर के बन्दे और आपस में भाई-भाई बनकर रहो।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने शिक्षा यह दी कि बदगुमानी को निकृष्टतम झूठ समझते हुए उससे बचो और इस मामले में अत्यन्त सतर्क रहो।
इससे यह भी मालूम हुआ कि सत्य और निष्ठा के गुणों से सुसज्जित होने के लिए केवल जिह्वा की रक्षा ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अपने विचारों को हर प्रकार की गन्दगी से बचाया जाए। अगर हमारे हृदय और हमारे विचारों में यह पवित्रता नहीं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि बुराई ने हमारे व्यक्तित्व को सुरक्षित नहीं रहने दिया है, और यह अत्यन्त चिन्ताजनक बात होगी।
इसके अतिरिक्त बदगुमानियों से समाज में घृणा और द्वेष का जो वातावरण उत्पन्न होता है उसे पवित्र, निर्मल और प्रीतिकर बनाना अत्यन्त दुष्कर होता है। ऐसा झूठ जो मौखिक हो, उसका खंडन किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होनेवाली ग़लतफ़हमियों को सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, लेकिन दिलों में जो बदगुमानियाँ बैठ जाती हैं उन्हें दूर करना आसान नहीं होता। साधारणतः आदमी को इसकी ख़बर कभी भी नहीं हो पाती कि कोई हमसे बदगुमान है। इसलिए बदगुमानी अगर झूठ है तो वह केवल झूठ ही नहीं है बल्कि निकृष्टतम झूठ है। उसकी बुराइयों का अन्दाज़ा करना भी साधारण परिस्थितियों में मुश्किल होता है। क़ुरआन में है—
“ऐ ईमान लानेवालो! बहुत-से गुमानों से बचो, क्योंकि कतिपय गुमान गुनाह होते हैं।" (49:12)
ईमानवालों को सदैव अच्छे गुमान और सदाशा से काम लेना चाहिए। अकारण और बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी के बारे में बुरी राय बना लेना इस्लामी सिद्धान्तों के अत्यन्त प्रतिकूल और समाज को तबाही के कगार पर ले जाने का प्रयास है।
यह जो कहा गया कि टोह में न पड़ो, इसका अर्थ यह है कि करने के बहुत-से काम हैं, तुम यह काम अपने ज़िम्मे लेकर अपनी अधमता और कुरुचि का प्रमाण न दो कि लोगों के दोष टटोलते फिरो और उनके रहस्यों को मालूम करने के चक्कर में पड़ो। मोमिन तो लोगों को अपमानित करने के बजाए उनकी मान-मर्यादा का रक्षक होता है। वह तो यथासम्भव लोगों के दोषों पर परदा डालने का प्रयास करता है। वह लोगों को अपमानित करने के बजाए उनके सुधार की चिन्ता करता है। मोमिन को हमेशा विशालहृदयता से काम लेना चाहिए। उसका प्रयास यह होना चाहिए कि यथासम्भव उसका दिल लोगों की तरफ़ से साफ़ हो। हदीस में है—
“जब किसी के बारे में तुम्हें कोई बुरा गुमान हो जाए तो उसकी खोजबीन न करो।" (अहकामुल-क़ुरआन लिल जस्सास)
अर्थात उस बदगुमानी को दूर करने का प्रयास करो न कि उसकी जाँच-पड़ताल द्वारा तुम्हें उसकी पुष्टि की चिन्ता होने लगे।
'न दूसरे से बढ़कर बोली बोलो', इसके लिए मूल में “ला तनाजशू" शब्द आया है। कोशकारों ने इसके कई अर्थ बताए हैं। 'नजश' के अर्थ हैं शिकार को भड़काना, शिकार को एक जगह से भड़काना ताकि वह दूसरी ओर चला जाए। 'ला तनाजशू' का अर्थ साधारणतः यह लिया गया है कि किसी माल की क़ीमत इस नीयत से मत बढ़ाओ कि दूसरा ख़रीदार प्रतिस्पर्धा में उसे अधिक मूल्य पर ख़रीद ले हालाँकि क़ीमत बढ़ानेवाले का उस माल को ख़रीदने का इरादा नहीं है। एक कथन यह है कि लोगों पर उच्चता प्राप्त करने का प्रयास न करो। एक दूसरे कथन के अनुसार इसका अर्थ यह है कि एक को दूसरे से नफ़रत न दिलाओ।
"न परस्पर शत्रुता या सम्बन्ध विच्छेद करो", इसके लिए मूल पाठ में “वला तदाबरू" आया है। इसका एक अर्थ यह भी लिया गया है कि आपस में पीठ पीछे एक-दूसरे की निन्दा न करो।
“भाई-भाई बनकर रहो” का अर्थ यह है कि तुम न झूठे बनो और न ईर्ष्यालु और उपद्रवकारी बनो। तुम तो ईश्वर के सच्चे बन्दे बनना पसन्द करो। इस प्रकार रहो जिस प्रकार रहना उसको पसन्द है। एक-दूसरे का बुरा चाहने के बजाए एक-दूसरे के भाई बन जाओ। यदि तुम सही अर्थों में ईश्वर के आज्ञाकारी बन्दे बन जाते हो और तुम्हारे बीच भाईचारे का रिश्ता स्थापित हो जाता है तो तुममें वे नैतिक बुराइयाँ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकतीं जिनसे बचने का निर्देश इस हदीस में दिया गया है।
यह हदीस अत्यन्त संग्राहक है। एक हदीस में इसे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस प्रकार कहा—
“आपस के नाते-रिश्ते को मत काटो, न परनिंदा करो और न परस्पर द्वेष और शत्रुता रखो, और न एक-दूसरे से ईर्ष्या करो, और अल्लाह के बंदे और भाई-भाई बन कर रहो।” (हदीस : मुस्लिम)
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मैं नहीं समझता कि अमुक-अमुक व्यक्ति हमारे धर्म की कोई बात जानते हों।" लैस कहते हैं कि ये दोनों कपटाचारी थे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इस्लाम प्राकृतिक धर्म है। एक ओर उसकी शिक्षा यह है कि लोगों से हमारे सम्बन्ध का आधार अच्छा गुमान, सदाशा और आत्मविश्वास हो, किसी से बदगुमानी न रखें। दूसरी ओर धर्म में यह भी अपेक्षित नहीं है कि जो चाहे वह हमारे इस अच्छे गुमान की नीति अपनाने से अनुचित लाभ उठाए और हमें धोखे पर धोखा देता चला जाए। जिसकी धर्म से विरक्ति और बेपरवाही स्पष्ट हो, जिसकी नीति ने साफ़ प्रकट कर दिया हो कि धर्म से उसका सम्बन्ध और सम्बद्धता किसी ज्ञान और मार्गदर्शन के कारण नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ दूसरी ही प्रेरणाएँ कार्यरत हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में ख़ुशगुमानी में पड़े रहने का कोई कारण नहीं है, बल्कि दूसरे लोग भी उसकी वास्तविक हैसियत से अवगत हो जाएँ तो अच्छा है ताकि वे कभी उसके धोखे में न आ सकें।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का बयान है कि एक दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेरे पास आए और कहा—
"अमुक-अमुक व्यक्ति के सम्बन्ध में मेरा गुमान यह नहीं है कि वे दोनों हमारे दीन को, जिसपर हम हैं, जानते हों।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : इस हदीस और इससे पहले की हदीस से मालूम हुआ कि धर्म के लिए ज्ञान आवश्यक है। ईश्वर का आज्ञापालन और उसकी बन्दगी ज्ञान के बिना सम्भव नहीं। जिस व्यक्ति को यह ख़बर ही न हो कि धर्म क्या है? उसकी आत्मा क्या है? वह अपने अनुयायियों को किन विचारों से सुसज्जित देखना चाहता है? उसे कौन-से कर्म प्रिय और कौन से अप्रिय हैं? जिस व्यक्ति को यह कुछ मालूम न हो उसके विषय में यह कैसे समझा जा सकता है कि धर्म को उस व्यक्ति ने भली-भाँति समझकर अपनी पूर्ण चेतना के साथ अपनाया होगा और उसके सच्चा मोमिन होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।
टोह
(1) हज़रत मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते सुना है—
“तुम अगर लोगों के छिपे हुए हालात जानने के पीछे पड़ोगे तो उन्हें बिगाड़ दोगे या कम से कम उनको बिगाड़ के निकट पहुँचा दोगे।" (हदीस : अबू-दाऊद, अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : एक हदीस में “औरातिल मुस्लिमीन" के स्थान पर “औरातिन्नास” (लोगों के छिपे हुए हालात) के शब्द आए हैं।
मालूम हुआ कि टोह लोगों के सुधार का नहीं बल्कि उनके बिगाड़ का कारण बनता है। लोगों की बुराइयों की तलाश और उनके दोषों का प्रचार उनको निर्भीक बना सकता है। उनमें लज्जा शेष रहे, इसलिए अनिवार्य है कि उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा का अत्यन्त ध्यान रखा जाए। अगर हमने किसी का रहस्य उघाड़कर उसे समाज में नग्न कर दिया तो फिर वह सोच सकता है कि अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है जिसकी रक्षा के लिए हम प्रयत्नशील हों। नैतिक मृत्यु से बढ़कर किसी मृत्यु की हम दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं—
“जिस किसी ने किसी का छिपा हुआ दोष देख लिया और उसपर परदा डाल दिया तो यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति ने एक जीवित गाड़ी हुई बच्ची को मृत्यु से बचा लिया।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद; उक़बा-बिन-आमिर से उल्लिखित)
(2) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इससे रोका है कि कोई व्यक्ति अपने घर रात को इस उद्देश्य से आए कि वह घरवालों की चोरी और विश्वासघात को पकड़े या उनके दोष और भेद को ढूंढे। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : बुरा गुमान करना, और वह भी अपने परिवारवालों के प्रति, अत्यन्त अनुचित और अशोभनीय है। इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसा करने से मना किया है। घर में यदि एक को दूसरे पर भरोसा न हो तो जीवन की सम्पूर्ण सुन्दरता कटुता में परिवर्तित हो जाए। ऐसा अन्दाज़ अपनाना जिससे स्त्री का दिल टूटे, अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट करना है।
(3) हज़रत मिक़दाम-बिन मअदीकरब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“शासक जब लोगों में सन्देह की बात ढूँढता है तो वह उनको बिगाड़ देता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने राज्य की शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र का उल्लेख किया है। राज्य की अखंडता और लोक-कल्याण के लिए अनिवार्य है कि शासक वर्ग और जनता के बीच विश्वास का वातावरण पाया जाता हो। पदाधिकारियों को अपनी जनता पर जो भरोसा और विश्वास हो उसे पदाधिकारियों की ओर से समय-समय पर प्रकट होते रहना चाहिए। इसका जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन शासक वर्ग अगर संकीर्णता से काम लेता है और उसे किसी विशेष गरोह या जनता की वफ़ादारी सन्दिग्ध प्रतीत होती है, फिर वह उनपर आक्षेप लगाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्टों से पीड़ित रखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि इस नीति के साथ किसी सुदृढ़ शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब देश में बेचैनी और असन्तोष का वातावरण व्याप्त होगा तो इसका परिणाम शासक वर्ग के लिए भी हितकर नहीं हो सकता।
इस हदीस से जहाँ यह मालूम होता है कि लोगों के रहस्यों की जिज्ञासा और उनके अवगुणों की टोह में नहीं पड़ना चाहिए वहीं इसमें इस बात की ओर भी संकेत पाया जाता है कि अगर लोगों में वास्तव में कुछ दोष हों तो यथासम्भव उन्हें अनदेखा करने का प्रयास किया जाए और उनके सुधार के प्रयास का कोई अच्छा तरीक़ा अपनाया जाए।
दोषान्वेषण और लज्जित करना
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मिम्बर पर आए और उच्च स्वर में कहा—
“ऐ वे लोगो, जिनका इस्लाम केवल उनकी अपनी ज़बान पर है और ईमान अभी उनके दिलों में नहीं उतरा है! मुसलमानों को दुख न पहुँचाओ, उन्हें शर्म न दिलाओ और उनमें दोष निकालने के पीछे न पड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई के दोष निकालने के पीछे पड़ेगा, अल्लाह उसके दोषों के पीछे पड़ जाएगा और जिस किसी के दोषों के पीछे ईश्वर पड़ जाएगा, वह उसे अपमानित करके रहेगा, यद्यपि वह अपने घर के अन्दर ही क्यों न बैठ रहे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह बात ईमान और इस्लाम के सरासर विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति अपने मुसलमान भाई को कष्ट पहुँचाए, उसे लज्जित करे और उसके दोष निकालने की ताक में रहे। इस्लामी शरीअत की दृष्टि से यह अत्यन्त अप्रिय बात है कि आदमी दूसरों में दोष निकालने और कमज़ोरी तलाश करने में रुचि ले। कौन व्यक्ति है जिसमें कोई न कोई कमज़ोरी न पाई जाती हो। किसी सज्जन व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त बुरी बात होगी कि दूसरों के दोषों की छानबीन में अपना मूल्यवान समय नष्ट करे। बल्कि उसे अगर किसी का कोई दोष और चूक मालूम हो भी जाए तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को निन्दित करने और उसको लोगों की नज़रों से गिराने के उद्देश्य से उसके दोषों की तलाश में रहता है तो वह स्वयं अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी गरिमा को बाक़ी नहीं रख सकता। ईश्वर इसका दंड उसे संसार में ही देगा, और दूसरों को अपमानित करने की मनोवृति रखनेवाला अन्ततः ख़ुद ही अपमानित और निन्दित होकर रहेगा। ईश्वर का व्यवहार उसके साथ वही होगा जैसा व्यवहार वह अपने भाई के साथ करेगा।
यहाँ यह बात दृष्टि में रहनी चाहिए कि खुले अपराधियों की बात इससे बिल्कुल भिन्न है। उसके अपराधों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बल्कि ऐसे अपराधी के विरुद्ध तो आवाज़ उठाई जाएगी। जब उसे स्वयं अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है तो दूसरा कौन उसे गरिमावान बना सकता है।
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि एक अवसर पर मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कह बैठी कि आपको तो बस वही सफ़ीया काफ़ी हैं जो ऐसी और ऐसी हैं (अर्थात छोटे क़द की हैं)। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम ने ऐसी बात कही है कि अगर उसे समुद्र में घोल दिया जाए तो उसे भी प्रभावित करके रहे।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात किसी को तुच्छ ठहराने के उद्देश्य से किसी के बारे में इतनी-सी बात भी कहनी उचित नहीं जो हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के मुख से निकल गई। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि तुमने यह बात कहकर जो गुनाह किया है वह कोई साधारण गुनाह नहीं है। उसे अगर समुद्र में भी घोल दिया जाए तो वह उसे दूषित करके रहेगा। फिर सोचो कि यह चीज़ तुम्हारे सत्कर्मों और चारित्रिक सौन्दर्य के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पत्नियों के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त अच्छे और मधुर थे। लेकिन इनसान से कभी आसावधानी में ग़लती हो ही जाती है। इस चेतावनी के बाद हज़रत आइशा से फिर कभी इस प्रकार की चूक नहीं हुई। सहाबा का यही हाल था कि जिस ग़लती पर भी उन्हें सचेत किया गया, उसे उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी सर्वाधिक प्रिय पत्नी की अशोभनीय बात पर मौन नहीं रहते बल्कि उन्हें सचेत करते हैं। प्रेम और न्याय की अपेक्षा भी यही थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इस नीति में हमारे लिए बड़ी शिक्षा है।
परनिन्दा
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि दो रोज़ेदार आदमियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नमाज़ पढ़ चुके तो उनसे कहा—
“जाओ, दोबारा वुज़ू करो और अपनी नमाज़ फिर से पढ़ो और अपना रोज़ा पूरा करके दूसरे दिन यह रोज़ा फिर से रखो।” उन्होंने कहा, “क्यों ऐ अल्लाह के रसूल!” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "इसलिए कि तुमने अमुक व्यक्ति की पीठ-पीछे निन्दा की है।" (हदीस : बैहक़ी)
व्याख्या : इस हदीस से भली-भाँति अन्दाज़ा किया जा सकता है कि परनिन्दा से वुज़ू और नमाज़ और रोज़े का सौन्दर्य और तेज लुप्त हो जाता है। विद्वानों की दृष्टि में परनिन्दा से वुज़ू और रोज़ा टूटता तो नहीं मगर ईशभय रखनेवालों से अपेक्षित यही है कि अगर कोई परनिन्दा कर बैठे तो वह दोबारा वुज़ू कर ले। परनिन्दा ही नहीं अगर किसी ने अधिक हँसी-मज़ाक़ और निरर्थक बातें ही की हों तो भी उसके लिए उचित यही है कि वह वुज़ू को ताज़ा करले ताकि वह अन्धकार कुछ छट सके जिससे उसका हृदय व्यर्थ और अनर्गल बकवास के कारण आच्छादित हो गया है। रोज़ेदार के लिए भी आवश्यक है कि वह परनिंदा आदि से बचे और अपने रोज़े की सुरक्षा की ओर से कदापि निश्चिन्त न रहे।
(2) हज़रत अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“पीठ-पीछे निन्दा व्यभिचार से बढ़कर कठोर अपराध है।"
सहाबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, पीठ-पीछे निन्दा व्यभिचार से कठोर अपराध कैसे है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "आदमी व्यभिचार करता है, फिर तौबा करता है और अल्लाह उसकी तौबा स्वीकार करता है।" एक हदीस में है कि "फिर वह तौबा करता है और अल्लाह उसे क्षमा कर देता है लेकिन पीठ-पीछे निन्दा करनेवाले को अल्लाह क्षमा नहीं करता जबतक कि उसे वह व्यक्ति न क्षमा कर दे जिसकी उसने निन्दा की है।" और हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित हदीस के शब्द ये हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "व्यभिचार करनेवाला तौबा करता है और निन्दा करनेवाले के लिए तौबा नहीं।" (हदीस अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : जिन तीन रिवायतों का उल्लेख यहाँ किया गया है, उन्हें बैहक़ी ने शोअ'बिल ईमान में उद्धृत किया है। परनिन्दा को व्यभिचार से भी अधिक गम्भीर अपराध ठहराया गया है। क्योंकि परनिन्दा करनेवाले साधारणतः इसे हलकी चीज़ समझते हैं, इसलिए न वे इसपर लज्जित होते हैं और न तौबा से काम लेते हैं। जबकि व्यभिचार में लिप्त होनेवाला अनिवार्यतः अपने कृत्य पर लज्जित होता है और वह तौबा करता है और ईश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा चाहता है।
यह जो कहा गया कि "परनिन्दा करनेवाले के लिए तौबा नहीं", इसका अर्थ यह है कि परनिन्दा करनेवाले को साधारणतः तौबा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता इसलिए कि वह पीठ-पीछे निन्दा करने की बुराई और ख़राबी को महसूस नहीं करता। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि परनिन्दा करनेवाले व्यक्ति के मात्र तौबा करने से काम नहीं चल सकता जबतक कि वह व्यक्ति उसे क्षमा न कर दे जिसकी उसने निन्दा की है। उसकी तौबा की स्वीकृति उस व्यक्ति के क्षमा करने पर निर्भर करती है जिसकी उसने निन्दा की है।
(3) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे सहाबा में से कोई मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न पहुँचाए क्योंकि मुझे यह बात पसन्द है कि जब मैं घर से निकलकर तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल साफ़ हो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : महान और प्रतापवान व्यक्तित्व का यही हाल होता है। जो व्यक्ति महान और उच्च होगा उसकी कामना और अभिलाषा यह होगी कि अपने साथियों की ओर से उसके हृदय में कोई द्वेष न हो ताकि जीवन भर वह उनसे राज़ी और प्रसन्न हो। इसके विपरीत संकीर्णहृदय व्यक्ति हमेशा इसकी टोह में रहता है कि वह लोगों की बुराइयों से अवगत हो। इसमें उसे एक विशेष प्रकार का रस मिलता है। इसे उसकी कुरुचि और अधमता के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो सच्चा सुधारक होगा उसका रुझान लोगों के सुधार और उनके दोषों को ढाँकने की ओर होगा। उसे लोगों के दोषों को उघाड़ने से अत्यन्त घृणा होगी।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तुम जानते हो कि परनिन्दा क्या है?” सहाबा ने कहा, “अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुम्हारा अपने किसी भाई की चर्चा इस प्रकार करना जो उसे अप्रिय हो।" कहा गया कि अगर वह बुराई वास्तव में मेरे भाई में हो जिसकी मैं चर्चा करूँ? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “अगर वह दोष उसमें है जो तुमने कहा है तो तुमने निन्दा की और अगर वह उसमें नहीं है तो तुमने उसपर मिथ्या दोषारोपण किया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : पीठ-पीछे किसी का कोई दोष बताना परनिन्दा है चाहे उस दोष का सम्बन्ध उस व्यक्ति के बाह्य जीवन से हो या उसके आन्तरिक जीवन से। अगर वह दोष वास्तव में उस व्यक्ति में नहीं पाया जाता जो कहनेवाला उससे सम्बद्ध कर रहा है तो यह निन्दा नहीं बल्कि आक्षेप और मिथ्यारोपण है जो परनिन्दा से बढ़कर गम्भीर क़िस्म का अपराध है।
परनिन्दा एक ऐसी बुराई है जिसकी समाज के बिगाड़ और सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका है। किन्तु यह सामाजिक बुराई आज आश्चर्यजनक रूप से आम है। बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होंगे जिनमें यह बुराई न पाई जाती होगी।
यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी के दोषों की चर्चा केवल मुख से ही नहीं अपितु संकेतों और इशारों से भी सम्भव है। अपने भाई को तुच्छ ठहराना और उसके व्यक्तित्व को धूमिल करना हर हाल में अवैध है। बिना किसी मजबूरी और अपरिहार्य कारण के किसी के दोषों को उसके मुँह पर भी बताना घोर पाप है। इसलिए कि यह लज्जा और सौम्यता के प्रतिकूल है। इसे पाषाणहृदयता और उत्पीड़न के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता।
कतिपय परिस्थितियों में किसी के अवगुणों या उसकी किसी कमज़ोरी को प्रकट करना अपरिहार्य हो जाता है। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियों का हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे। इन विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी के पीठ-पीछे उसके दोषों की चर्चा परनिन्दा ही कहलाएगी।
(5) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब मुझे मेराज हुई तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाख़ून ताँबे के थे, जिनसे वे अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच-खरोंच रहे थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो लोगों का माँस खाया करते थे और उनकी आबरूओं के पीछे पड़े रहते थे।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : “जो लोगों का माँस खाया करते थे" अर्थात पीठ-पीछे उनकी निन्दा करते रहते थे, उनकी मान-मर्यादा के पीछे पड़े रहते थे। अर्थात उनके लिए अशिष्ट और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते थे। और इस प्रकार उनकी मान-मर्यादा से खेलते थे। इन्होंने लोगों की मर्यादाओं को रौंदकर उनके हृदयों को व्यथित और उनके चेहरों को आहत किया। अतः इनके लिए यही दंड उचित है कि अब ये स्वयं अपने हाथों से अपने सीनों और अपने चेहरों को विकृत और आभाहीन करें।
(6) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मृत्यु-प्राप्त लोगों को बुरा मत कहो क्योंकि जो कुछ उन्होंने आगे भेजा वे उसे पा चुके।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात किसी की मृत्यु के बाद उसकी निन्दा करना और भी बुरा है इसलिए कि जो कुछ उसने दुनिया में किया है अब वह स्वयं उसके परिणामों को भोग रहा है। अब उसकी निन्दा एक अपकर्म के सिवा कुछ नहीं।
(7) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मैं नहीं समझता कि अमुक और अमुक व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान रखते हों।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात वे सत्यधर्म से नितान्त अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। यहाँ अंदाज़ प्रकटतः निन्दा का मालूम होता है लेकिन यह निन्दा नहीं है क्योंकि किसी की पीठ पीछे उसकी किसी कमज़ोरी और त्रुटि को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है जिसका उद्देश्य वासनातृप्ति न हो बल्कि लोगों को उसकी दुष्टता से सुरक्षित रखना या उन्हें सचेत करना हो कि वे उसके ज्ञान और संयम के ऊपरी दावे से किसी धोखे में न पड़ जाएँ।
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति या गरोह के अवगुणों को उसके पीठ-पीछे प्रकट करना उचित होता है, उदाहरणस्वरूप किसी अत्याचारी की अत्याचारपूर्ण नीति से शासक को अवगत कराना ताकि वह उसे अत्याचार से बाज़ रखने का उपाय कर सके। इसी प्रकार शादी के सम्बन्ध में अगर मश्विरा मांगा जाए तो मश्विरा माँगनेवाले को बता दे कि जिस व्यक्ति से वह रिश्ता क़ायम करने जा रहा है वह चरित्र और नैतिकता की दृष्टि से कैसा है। इसी प्रकार हदीस के रावियों के हालात के प्रकटीकरण के सिलसिले में आवश्यक समझा गया है कि अगर उनमें से किसी की कुछ कमज़ोरियाँ सामने आती हैं तो उन कमज़ोरियों को कदापि न छिपाए ताकि उसके द्वारा वर्णित हदीस के बारे में सही मत अपनाया जा सके। हदीसशास्त्रियों ने उन रावियों पर जो विश्वसनीय और न्यायशील न थे जिरह की है और यह जिरह उन्होंने शरअ् अर्थात धर्म की अपेक्षा के अंतर्गत ही की है।
सारांश यह कि किसी धार्मिक, सामाजिक और नैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति या गरोह के दोषों से परदा उठाना निन्दा में सम्मिलित नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में तो यह परदा उठाना नितान्त अत्यावश्यक हो जाता है। इमाम नव्वी (रहमतुल्लाह अलैह) ने ऐसी छः परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके कारण किसी की बुराई या ऐब बयान करना अवैध नहीं रहता।
(8) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“परनिन्दा का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) यह है कि उस व्यक्ति के लिए क्षमादान की प्रार्थना की जाए जिसकी निन्दा की गई हो।” (हदीस : जामेअ् सग़ीर)
व्याख्या : कतिपय विद्वानों का विचार है कि जिसकी निन्दा की गई है उसके पक्ष में क्षमादान की प्रार्थना उसी स्थिति में होगी जबकि उस व्यक्ति को जिसकी निन्दा की गई है, उस निन्दा की ख़बर न हो। और अगर उसे निन्दा की ख़बर मिल चुकी है तो फिर यह अनिवार्य हो जाता है कि निन्दा करनेवाला उससे अपनी ग़लती क्षमा करा ले। अलबत्ता यदि उससे क्षमा माँगने की सम्भावना शेष न रही हो, उदाहरणार्थ उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो फिर इस स्थिति में तौबा और ईश्वर से क्षमायाचना करे और ईश्वर से यह आशा रखे कि ईश्वर उस व्यक्ति को इसपर राज़ी कर देगा कि वह अपनी निन्दा को क्षमा कर दे।
चुग़ली
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो कहा—
“इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है, और यह अज़ाब उनपर ज़ाहिर में किसी बहुत बड़े गुनाह के कारण नहीं हो रहा है। यह क़ब्रवाला अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और यह चुग़ली खाता फिरता था।" फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक ताज़ा शाख़ मँगाई और उसके दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा इसपर और दूसरा टुकड़ा उसपर गाड़ दिया और कहा, "उम्मीद है कि दोनों के अज़ाब में कमी होगी जब तक कि ये सूख न जाएँ।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : "यह अज़ाब उन पर ज़ाहिर में किसी बहुत बड़े गुनाह के कारण नहीं हो रहा है", मूल में “वमा-फ़ी कबीर" के शब्द आए हैं। बुख़ारी की एक दूसरी हदीस में “वमा युअज़्ज़िबानि फ़ी कबीरिन बला इन्नहू कबीर” के शब्द आए हैं। अर्थ यह है कि अज़ाब प्रत्यक्षतः किसी बड़े गुनाह के कारण नहीं हो रहा था। वे दुनिया में उनकी ओर से बेपरवाह थे। उनको कोई बड़ा गुनाह नहीं समझते थे लेकिन वास्तव में ये गुनाह हल्के और साधारण न थे। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि ये गुनाह ऐसे न थे कि इनसे बचना उनके लिए कठिन और दुष्कर कार्य था। अगर वे चाहते तो सरलतापूर्वक इनसे बच सकते थे। निस्संदेह उन्होंने सतर्कता से काम नहीं लिया। उनका यह अपराध साधारण नहीं है।
शाखाएँ जब तक हरी रहती हैं वे ईश्वर का स्मरण और उसकी तस्बीह करती रहती हैं। उनके इस स्मरण के कारण अज़ाब में कमी की आशा होती है। इस स्मरण और तस्बीह की वास्तविकता चाहे हम समझ न सकें लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि दुनिया में जहाँ कहीं और जिस सूरत में भी सुन्दरता, ताज़गी, खिलावट और निर्मलता पाई जाती है वह ईश्वरीय गुणों ही की प्रतिच्छाया है। ईश्वरीय गुणों के प्रतिबिंब के बिना हम किसी सौन्दर्य और शुभ की कल्पना नहीं कर सकते।
(2) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“जन्नत में चुग़लख़ोर व्यक्ति प्रविष्ट न होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मुस्लिम की एक हदीस में “क़त्तातुन" के स्थान पर “नम्मामुन" शब्द आया है। दोनों का एक ही अर्थ है अर्थात चुग़लख़ोर। जो व्यक्ति चुग़ली खा-खाकर समाज को बिगाड़ने और उसे नरकतुल्य बनाने के प्रयास में लगा हो, वह उस स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकेगा जहाँ बिगाड़ और उपद्रव नहीं और न जहाँ ईर्ष्या और द्वेष पाया जाता है। जहाँ ऐसी कोई चीज़ देखने को न होगी जो नैतिक ह्रास और नीचता का प्रतीक हो।
किसी की ऐसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चुग़ली है जिसके कारण वह व्यक्ति उससे क्रुद्ध या बदगुमान हो जाए और उनके आपसी सम्बन्ध ख़राब हो जाएँ। जो चीज़ें भी पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने वाली और द्वेष और शत्रुता को हवा देनेवाली हैं इस्लाम उनको निकृष्टतम पापों में से एक पाप घोषित करता है। इसलिए कि इस प्रकार की चीज़ें उन महान उद्देश्यों के विरुद्ध हैं जिनको नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाओं में मौलिक महत्व दिया गया है। जैसे भाईचारा, प्रेम, सभ्यता और पारस्परिक सम्बन्धों का बनाव और सौन्दर्य, आदि।
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं तुम्हें बताता हूँ कि निकृष्टतम मिथ्या दोषारोपण क्या है। यह वह चुग़ली है जो लोगों के बीच शत्रुता डाल दे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस में उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते और चुग़ली खाते फिरते हैं। ऐसे लोग वास्तव में समाज के शत्रु होते हैं। लोगों के बीच फ़ितना और फ़साद के बीज बोना ही उनका सर्वाधिक प्रिय कार्य हुआ करता है।
द्वेष
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सोमवार और गुरुवार के दिन स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं और फिर ऐसे बन्दे को क्षमा कर दिया जाता है जो ईश्वर के साथ किसी चीज़ को शरीक न करता हो, सिवाय उस व्यक्ति के जिसका अपने भाई के साथ द्वेष और शत्रुता हो, और आदेश होता है कि इन्हें देखते रहो यहाँ तक कि ये परस्पर मिल जाएँ, इन्हें देखते रहो यहाँ तक कि ये परस्पर मिल जाएँ।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम में एक दूसरी हदीस हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से यह उल्लिखित है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"सप्ताह में दो बार अर्थात सोमवार और गुरुवार को लोगों के कर्म प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर प्रत्येक मोमिन बन्दे को क्षमा कर दिया जाता है सिवाय उस बन्दे के जो अपने और अपने भाई के बीच द्वेष और शत्रुता रखता हो। अतः आदेश होता है कि इन्हें छोड़े रखो (इनके मामले को स्थगित रखो) यहाँ तक कि ये पलटें और शत्रुता से बाज़ आ जाएँ।" (हदीस : मुस्लिम)
ये हदीसें बताती हैं कि निरन्तर लोग सत्य की दृष्टि में रहते हैं और सप्ताह में विशेष रूप से दो बार यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति की क्या अवस्था है। कौन स्वर्ग और क्षमा का अधिकारी है और किसके लिए स्वर्ग वर्जित है। जिसके लिए न तो स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और न उसे क्षमा किया जाएगा, सिवाय इसके कि वह अपना सुधार कर ले और अपना मामला दुरुस्त कर ले। ईमान के अभाव में तो मुक्ति और क्षमा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन मोमिन व्यक्ति के लिए भी उस समय तक स्वर्ग के द्वार बन्द रहते हैं और उसके लिए क्षमादान भी स्थगित रहता है जबतक कि वह ईमान की अपेक्षाओं को पूरा न कर ले। या दूसरे शब्दों में ऐसा जीवन न अपना ले जो जीवन स्वर्गवालों का होता है। हम जानते हैं कि स्वर्गवालों में परस्पर कोई द्वेष और शत्रुता न होगी। उनके हृदय इस तरह की चीज़ों से सर्वथा मुक्त होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वर्ग उनके लिए है जो अपने दिलों से अपने भाइयों का बुरा न चाहते हों और न उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते हों। यही कारण है कि जिनके दिलों में अपने भाइयों के लिए कपट और द्वेष होता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार बन्द ही रखे जाते हैं। हालाँकि ये द्वार सप्ताह में दो बार खुलते हैं और क्षमायोग्य लोगों को क्षमा कर दिया जाता है और उन्हें ऊँचे दर्जे दिए जाते हैं।
इन हदीसों से यह मालूम हुआ कि सोमवार और गुरुवार को बहुतायत से ईश्वरीय अनुकम्पा का अवतरण होता है जो उन बन्दों के क्षमादान और मुक्ति का कारण बनती है जो इसके पात्र होते हैं। इन अवसरों पर लोगों के कर्मों का भी निरीक्षण किया जाता है ताकि यह निर्णय किया जा सके कि वे भाग्यशाली लोग कौन हैं जो ईश्वरीय क्षमा और अनुकम्पा के पात्र और उसके स्वर्ग के हक़दार हैं और कौन हैं जो ईश-दयालुता से वंचित रहेंगे और वे कौन हैं जिनसे यह आशा की जा सकती है कि शायद वे अपना सुधार कर लें और ईश्वरीय अनुकम्पा उन्हें अपने आश्रय में ले ले।
दूसरों की हानि से प्रसन्न होना
(1) हज़रत वासिला (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम अपने भाई की मुसीबत पर खुशी प्रकट न करो कि (तुम्हारे) इस व्यवहार के कारण ईश्वर उसपर दया करे और तुम्हें उस मुसीबत में डाल दे।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मूल अरबी में शब्द ‘शमातत’ प्रयुक्त हुआ है। अपने किसी भाई को मुसीबत में फँसा देखकर प्रसन्न होना 'शमातत' कहलाता है। ईर्ष्या और द्वेष की भाँति शमातत भी नैतिक गिरावटों में से एक है। शमातत और विशालहृदयता परस्पर विरोधी गुण हैं। शमातत अल्लाह को इतना अप्रिय है और वह इससे इतना क्रुद्ध होता है कि बहुधा दुनिया ही में वह इसका दंड दे देता है। और वह इस प्रकार कि विपत्ति में फँसे व्यक्ति को तो वह विपत्ति से निकाल लेता और उसकी विपत्ति दूर कर देता है और जो व्यक्ति उसकी विपत्ति पर ख़ुशियाँ मना रहा था उसे संकटग्रस्त कर देता है।
ईर्ष्या
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईर्ष्या से बचो, क्योंकि ईर्ष्या नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है या कहा 'घास को खा लेती है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात आग जिस प्रकार लकड़ी या घास को जलाकर राख कर देती है, ठीक यही हाल ईर्ष्या की आग का है। किसी के दिल में जब यह आग भड़कती है तो वह उसके धार्मिक और नैतिक व्यक्तित्व को विनष्ट करके रहती है। किसी में ईर्ष्या के रोग का पाया जाना उसके चरित्र और व्यक्तित्व के पतन का खुला प्रमाण है। जब चरित्र ही नहीं रहा तो उसके सत्कर्मों का क्या महत्व शेष रह सकता है? किसी के सत्कर्मों से इसका संकेत मिलता है कि इस्लाम आदमी को जैसा चरित्रवान देखना चाहता है उसकी उससे आशा की जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी में ईर्ष्या जैसा रोग पाया जाता है तो यही एक चीज़ सम्पूर्ण आशाओं पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। मानव को एक-दूसरे का ईर्ष्यालु बनकर नहीं बल्कि हमदर्द और शुभचिन्तक बनकर रहने की शिक्षा दी गई है। इनसान के व्यक्तिगत विकास के लिए इससे अच्छी किसी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। इस शिक्षा के विपरीत जो नीति भी इनसान अपनाएगा वह उसके चरित्र और व्यक्तित्व के लिए घातक विष से कम न होगा।
इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हर समय उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की चिन्ता में पड़ा रहता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। और कुछ नहीं तो वह उसकी निन्दा ही करता रहता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। और इस प्रकार वह अपने दिल की आग बुझाना चाहता है। इसका नतीजा यह होगा कि उसकी नेकियाँ उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी जिसकी वह संसार में निन्दा करता फिरता था। इस प्रकार नेकियों के नष्ट होने के लिए एक ईर्ष्या का रोग ही पर्याप्त हो सकता है।
(2) हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम्हारी ओर अगली उम्मतों की बीमारी चली आई। वह बीमारी ईर्ष्या और द्वेष की है। यह मूँड देनेवाली है। मैं यह नहीं कहता कि यह बाल को मूँड देती है बल्कि यह धर्म को मूँडकर रख देती है।" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस बात की सूचना अल्लाह ने दे दी थी कि यद्यपि ईश्वर की विशेष अनुकम्पा से ईमानवालों के हृदय परस्पर मिले हुए हैं और वे भाई-भाई हो गए हैं और पुराने झगड़ों को उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है लेकिन द्वेष और ईर्ष्या की बीमारी पिछली उम्मतों की भाँति आगे चलकर आपकी उम्मत को भी पकड़ लेगी। इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुसलमानों को सावधान किया कि इसकी ओर से सचेत रहें और अपने दिलों को इस लानत से बचाए रखने की कोशिश से कभी ग़ाफ़िल न हों। वे ईर्ष्या और द्वेष को साधारण बात न समझें। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी का धर्म और ईमान चौपट होकर रह जाता है।
दोषारोपण
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना कि—
“जिस व्यक्ति ने अल्लाह की किसी 'हद' (ईश-निर्धारित दंड) को रोकने के लिए सिफ़ारिश की तो उसने ईश्वर का विरोध मोल लिया और जिसने जानते-बूझते नाहक़ झगड़ा किया तो वह हमेशा ईश्वर के क्रोध का भागी रहेगा जब तक कि वह उस झगड़े से हाथ न खींच ले। और जिस किसी ने किसी मोमिन के विषय में वह बात कही जो (बुरी बात) उसमें न थी तो अल्लाह उसके आवास की व्यवस्था नरकवासियों के मैल-कुचैल और कीचड़ में कराएगा यहाँ तक कि जो कुछ उसने कहा उससे वह तौबा करले।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : एक हदीस में इनके अतिरिक्त शब्द भी आए हैं—
“और जिस किसी ने किसी झगड़े में नाहक़ सहयोग किया तो वह निश्चय ही ईश्वरीय कोप का भाजन बनेगा।"
“अल्लाह की हद को रोकने के लिए सिफ़ारिश की" अर्थात न्यायाधीश तक मुक़द्दमा पहुँच जाने के बाद अगर कोई इस बात की सिफ़ारिश और प्रयास करता है कि अपराधी पर हद क़ायम न हो, उदाहरणार्थ चोर का हाथ न काटा जाए या व्यभिचारी पर शरई हद जारी न हो तो ऐसा व्यक्ति कोई साधारण ग़लती नहीं कर रहा है बल्कि वह तो ईश्वर का विरोध कर रहा है।
इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि किसी मोमिन पर झूठा आरोप लगाना घोर पाप है। कोई व्यक्ति आज किसी मोमिन पर गन्दगी और कीचड़ उछालता है तो कल उसे नरकवालों के मैल-कुचैल और कीचड़ में वास करना होगा। अब इस बुरे परिणाम से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि वह तौबा करे और अपनी इस बुरी हरकत से बाज़ आ जाए और क्षतिपूर्ति की चिन्ता करे अर्थात दुनिया के जीवन ही में उस मोमिन व्यक्ति से क्षमा माँग कर उसे राज़ी कर ले।
विश्वासघात
(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मोमिन की प्रकृति में प्रत्येक आदत और दुर्गुण की सम्भावना है सिवाय विश्वासघात और झूठ के।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मोमिन है तो दूसरी कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ तो उसमें हो सकती हैं लेकिन विश्वासघात और झूठ जैसे कपटाचार के दुर्गुण उसमें नहीं पाए जा सकते। संयोगवश मोमिन से विश्वासघात और झूठ जैसी बुराइयाँ भी हो सकती हैं लेकिन यह सम्भव नहीं कि विश्वासघात और झूठ को वह अपनी पहचान बना ले। अगर किसी व्यक्ति के अन्दर ये दोनों दोष रच-बस गए हैं और वह ईमान का दावेदार भी है तो समझ लेना चाहिए कि इस दावे के बावजूद अभी तक ईमान की हक़ीक़त से उसका हृदय अपरिचित ही है।
(2) हज़रत सौबान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस व्यक्ति को इस हाल में मृत्यु आए कि वह अहंकार, विश्वासघात और ऋण से मुक्त हो तो वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा, दारमी)
व्याख्या : विश्वासघात के लिए हदीस के मूल में असल शब्द 'ग़ुलूल' आया है। वितरण से पहले ग़नीमत के माल (विजित धन) में चोरी को ‘ग़ुलूल' कहते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए है जो उच्च चरित्र और व्यक्तित्व के मालिक हों और ऐसे न हों जिनपर विश्वास न किया जा सके।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि प्रतापवान ईश्वर कहता है कि जब तक किसी कारोबार के दो साझीदार परस्पर विश्वासघात न करें, मैं उनके साथ रहता हूँ लेकिन जब एक साझीदार दूसरे के साथ विश्वासघात करता है तो मैं उन दोनों के बीच से निकल जाता हूँ। (एक हदीस में है कि) और फिर शैतान आ जाता है। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि जब तक किसी व्यवसाय के साझीदार आपस में एक-दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हैं और विश्वासघात से दूर रहते हैं, ईश्वर की सहायता उन्हें प्राप्त रहती है। ईश्वर उनके कारोबार में उन्नति देता है। लेकिन जब उनकी नीयतों में फ़र्क़ आ जाता है और कारोबार के साझियों में से हरेक केवल अपना लाभ देखता है और दूसरे के साथ विश्वासघात और अन्याय करने लगता है ताकि अधिक से अधिक लाभ अकेले उसी के हिस्से में आए तो ऐसी अवस्था में ईश्वर की रहमत उनसे अलग हो जाती है और वह अपनी मदद का हाथ खींच लेता है। फिर शैतान को इसका पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता है कि वह उनके आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ दे और उनके कारोबार को तबाही के रास्ते पर डाल दे।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी ने तुम्हें विश्वासयोग्य समझा है उसपर अपना विश्वासपात्र होना सिद्ध करो और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे तुम उसके साथ विश्वासघात की नीति न अपनाओ।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात किसी के साथ विश्वासघात की नीति कदापि न अपनाओ यहाँ तक कि उस व्यक्ति के साथ भी विश्वासघात न करो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है।
अरबी भाषा में 'अमानतुन' के अर्थ हैं विश्वासपात्र होना। ऐसा होना कि लोगों को पूर्ण विश्वास हो कि यह व्यक्ति हमारा हक़ नष्ट नहीं कर सकता। क़ुरआन में है—
“अतएव यदि तुममें से एक, दूसरे पर भरोसा करे, (और इस भरोसे पर एक दूसरे को क़र्ज़ दे दे) तो जिसपर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वह अपने विश्वासपात्र होने को सिद्ध कर दे (और क़र्ज़ देने वाले के भरोसे को आघात न पहुँचाए)।” (2:283)
(5) हज़रत सुफ़ियान-बिन-उसैद हज़रमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
"यह बहुत बड़ा विश्वासघात है कि तुम अपने भाई से कोई झूठी बात कहो और वह तुम्हें इस बयान में सच्चा समझता हो।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात विश्वासघात का सम्बन्ध केवल धन-सम्पत्ति से ही नहीं है। विश्वासघात कई तरह के हो सकते हैं। इस हदीस में इसको भी विश्वासघात बल्कि बहुत बड़ा विश्वासघात ठहराया गया है कि कोई अपने भाई से झूठ कहे और उसका भाई उसे सच जाने। धोखा और विश्वासघात प्रत्येक स्थिति में गुनाह है लेकिन किसी के अच्छा गुमान रखने और भरोसा करने के बाद उससे अनुचित लाभ उठाकर उसे धोखा देना ऐसा विश्वासघात है जिसमें पाप की गम्भीरता अत्यन्त बढ़ जाती है। इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसे बहुत बड़ा विश्वासघात ठहराया है। अबू-दाऊद की एक दूसरी हदीस में है—
‘‘और जिस व्यक्ति ने अपने भाई को किसी कार्य का परामर्श दिया जिसके बारे में वह जानता है कि भलाई और अच्छाई उसके सिवा दूसरे काम में है तो निश्चय ही उसने विश्वासघात किया।”
अर्थात उसने भाई को ग़लत और हानिकर परामर्श देकर उसके साथ विश्वासघात किया। मालूम हुआ कि किसी को ग़लत मशवरा देना भी विश्वासघात है।
(6) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि मुझसे हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि जब ख़ैबर का युद्ध हुआ तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा आ-आकर कहने लगे कि अमुक व्यक्ति शहीद हो गया और अमुक व्यक्ति शहीद हो गया, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के पास से गुज़रे तो उसके बारे में भी यही कहा कि अमुक शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कदापि नहीं, मैंने तो उसको नरक की अग्नि में देखा है, इसके दंड में कि उसने एक चादर (या आपने यह कहा कि) एक इबा चुरा लिया था।" इसके बाद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ऐ ख़त्ताब के पुत्र, जाओ और लोगों में घोषणा कर दो कि स्वर्ग में केवल मोमिन प्रविष्ट होंगे।" यह बात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार कही। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने बाहर निकलकर यह घोषणा कर दी कि स्वर्ग में केवल मोमिन ही प्रविष्ट होंगे। और यह तीन बार कहा। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात जो ‘अलमोमिन' और वास्तव में ईमानवाले होंगे। यह हदीस उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस बात को अकसर भूल जाते हैं कि ईमान वास्तव में मोमिन के योग्य एक विशिष्ट चरित्र की माँग करता है। दुनिया एक व्यक्ति को मोमिन ही नहीं शहीद तक की उपाधि प्रदान कर सकती है लेकिन इस्लाम उसे मोमिन की उपाधि भी नहीं देता क्योंकि वह विश्वासघात का अपराधी था। मोमिन विश्वासघात का अपराधी क्योंकर होगा। वह कैसा मोमिन कि विजित धन में से चादर या इबा या कोई और चीज़ चुपके से ले ले और उसका अंतःकरण उसे इस बुरे कर्म से रोक न सके। यह वह मोमिन नहीं जिसकी प्रतीक्षा स्वर्ग करता है। अभीष्ट मोमिन तो वही लोग हो सकते हैं जो स्वतन्त्रता का आनन्द गुनाहों और विश्वासघातों में नहीं बल्कि आज्ञापालनों और वफ़ादारियों की अदायगी में महसूस करते हैं। स्वर्ग को ऐसे लोगों का इन्तिज़ार न होगा तो किसका होगा!
हड़पना और हथियाना
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“हरेक विश्वासघात करनेवाले और हड़प करनेवाले के लिए क़ियामत के दिन एक झंडा होगा जिसके द्वारा वह पहचान लिया जाएगा।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात ऐसा व्यक्ति क़ियामत के दिन अपमानित और तिरस्कृत होने से नहीं बच सकता। दूर ही से लोग झंडा देखकर पहचान लेंगे कि यह व्यक्ति लोगों की चीज़ें हड़प लेता था और उनके साथ विश्वासघात करता था।
(2) हज़रत वायल-बिन-हुज्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जो व्यक्ति अत्याचारी बनकर किसी की भूमि छीन लेगा वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वह उसपर अत्यन्त क्रुद्ध होगा।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : भाग्यशाली है वह व्यक्ति जो क़ियामत के दिन ईश्वर से भेंट करे तो उसका ईश्वर उससे राज़ी और प्रसन्न हो। लेकिन हड़पनेवाले अत्याचारी के भाग्य में उस दिन ईश्वरीय प्रकोप के सिवा और कुछ न आ सकेगा। जिसपर ईश्वर का प्रकोप हो उसका क्या परिणाम होगा, इसे प्रत्येक व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सकता है।
(3) हज़रत अबू-उमामा अयास-बिन-सअलबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति किसी मुसलमान का हक़ झूठी क़सम खाकर छीन लेगा तो ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर ने नरक अनिवार्य कर दी है और स्वर्ग को उसपर हराम (वर्जित) कर दिया है।" एक व्यक्ति ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल, अगर वह चीज़ थोड़ी हो?” आपने कहा, "हाँ अगर वह पीलू की टहनी ही हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : जो व्यक्ति किसी मुस्लिम का हक़ छीनता है और उसके लिए अनुचित उपाय करने में भी उसे कोई झिझक नहीं होती, यहाँ तक कि वह इसके लिए झूठी क़स्में भी खा लेता है, वह आख़िरत के जीवन में स्वर्ग का नहीं नरक का भागी ठहरेगा यद्यपि उसने कोई साधारण चीज़ ही क्यों न हड़प ली हो। पीलू की एक टहनी यद्यपि साधारण सी चीज़ है लेकिन उसे छीनकर उसने अपनी जिस कुचरित्रता का परिचय दिया वह कोई साधारण अपराध नहीं है जिसे नज़रअन्दाज़ किया जा सके।
ज़बान की लापरवाही
(1) हज़रत सहल-बिन-साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति मुझे अपने दोनों जबड़ों और दोनों पैरों (टाँगों) के बीच की चीज़ की ज़मानत दे तो मैं उसे स्वर्ग की ज़मानत देता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात जो व्यक्ति अपनी जीभ और आबरू की रक्षा की ज़मानत दे तो मैं उसे स्वर्ग की ज़मानत देने को तैयार हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़बान और शर्मगाह (गुप्तांग) की सुरक्षा करता है, न वह ज़बान के इस्तेमाल करने में मर्यादाओं की उपेक्षा करता है और न व्यभिचार के निकट जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी ठहरेगा। स्वर्ग उन ही लोगों के लिए है जो पवित्र आत्मा और पवित्र आचरण वाले होते हैं और जिन की ज़बानें इसकी गवाही देती हैं कि वे बेपरवाह और अनुत्तरदायी क़िस्म के लोग नहीं हैं। वे जो कुछ कहते हैं, ख़ूब सोच-समझकर कहते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी के झूठा होने के लिए यही पर्याप्त है कि वह हर वह बात जो सुने, वर्णन कर दे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात आदमी चाहे जान-बूझकर झूठ न बोले लेकिन अगर वह जो कुछ लोगों से सुनता है उसकी पुष्टि के बिना बयान करने लगता है तो केवल यही चीज़ उसके झूठा होने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कि सुनी-सुनाई बातों में नहीं मालूम कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो ग़लत और निराधार होंगी। अब जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी ज़बान पर झूठी बात न आए और किसी सूरत में भी वह झूठा सिद्ध न हो तो उसके लिए अनिवार्य है कि वह पुष्टि के बिना लोगों से सुनी-सुनाई बातों को कदापि न फैलाए।
(3) हज़रत बिलाल-बिन-हारिस मुज़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“आदमी अल्लाह की प्रसन्नता की एक बात कह देता है, वह नहीं जानता कि उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचेगा और उसके कारण उसके लिए अल्लाह अपनी रज़ामन्दी क़ियामत के दिन तक के लिए, जबकि वह उससे मिलेगा, लिख देता है। और एक आदमी अल्लाह की नाराज़ी की एक बात कह देता है, वह नहीं जानता कि उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचेगा और उसके कारण उसके लिए अल्लाह अपनी नाराज़ी क़ियामत के दिन तक के लिए, जबकि वह उससे भेंट करेगा, लिख देता है।" (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी की ज़बान उसके अपने अंजाम की मुख़बिर होती है। वह जो कुछ अपनी ज़बान से कहता है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कभी वह ज़बान से ऐसी बात कह जाता है जो ईश्वर की प्रसन्नता की होती है। स्वयं उसे उसके महत्व और उसके प्रभावों का अनुमान भी नहीं होता लेकिन जब वह अपने ईश्वर से मिलेगा तो यह हक़ीक़त खुलकर उसके सामने आ जाएगी कि ईश्वर की प्रसन्नता की जो बात उसके मुख से निकली थी उसके कारण ईश्वर ने अपनी रज़ामन्दी उसके लिए क़ियामत तक के लिए अनिवार्य कर दी थी। ईश्वर की रज़ामन्दी कदापि सामयिक न थी। वह ईश्वर से इस हाल में मिल रहा होगा कि उसका रब उससे राज़ी और अत्यन्त प्रसन्न होगा।
इसके विपरीत एक व्यक्ति अपने मुख से ईश्वर की नाराज़ी की कोई बात कह जाता है। उसे उसकी गम्भीरता और उसके दूरगामी परिणामों और प्रभावों का ध्यान भी नहीं होता हालाँकि उससे वह अपने ईश्वर को नाराज़ कर लेता है। और ईश्वर की यह नाराज़ी और क्रोध सामयिक नहीं होता। जब वह क़ियामत के दिन ईश्वर से मिलेगा तो वह उसे नाराज़ पाएगा। और यह हक़ीक़त उसपर प्रकट होगी कि अपनी ज़बान की असावधानी से उसने अपने प्रभु को नाराज़ कर रखा है।
नाराज़ ईश्वर को राज़ी करने की एक ही सूरत है कि दुनिया की ज़िन्दगी ही में बन्दा ईश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा माँग ले और गम्भीरतापूर्वक अपने सुधार की ओर ध्यान दे।
(4) हज़रत अबू-क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्रय-विक्रय में ज़्यादा क़स्में खाने से बचो, क्योंकि यह चीज़ कारोबार चला देती है और फिर मठ मार देती है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : ज़्यादा क़स्में खाने का अर्थ यह होता है कि आदमी के दिल में ईश्वर की महानता और उसके प्रताप का एहसास नहीं। यही कारण है कि वह मात्र भौतिक लाभ के लिए बार-बार ईश्वर को अपने वार्तालाप में खींच लाता है।
हल्फ़बाज़ी और क़स्में खाने से शुरू में कारोबार चल निकलने में आसानी हो सकती है लेकिन अन्ततः इससे कारोबार में बरकत शेष नहीं रहती। बुख़ारी की एक हदीस है—
"क़सम कारोबार के चलने का कारण बनती है लेकिन (अन्ततः) बरकत का मठ मार देती है।"
अर्थात प्रारम्भ में लोग किसी की क़स्मों पर विश्वास करके उससे अधिक से अधिक लेनदेन करने लगते हैं लेकिन अन्ततः यही चीज़ कारोबार की बरकत को समाप्त कर देती है। क़स्मों का ज़्यादा अधिक दिनों तक विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस चीज़ से कारोबार उन्नति करता है वह है दयानतदारी, ग्राहकों के साथ सदव्यवहार और उचित दर पर माल को बेचना। लेकिन कारोबार के बहाने अगर दुकानदार लोगों को धोखा देने, उनकी जेबें काटने और उनको लूटने लग जाए तो ऐसा दुकानदार ईश्वरीय अनुग्रह और सहायता से वंचित हो जाता है। देखा गया है कि ऐसे दुकानदार का माल नष्ट हो जाता है या फिर वह अपनी आमदनी को ऐसे कामों में लगा देता है जिसका लाभ उसे प्राप्त नहीं हो पाता।
फ़साद डालना
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दो आदमियों के बीच फ़साद डालने से बचो क्योंकि यह चीज़ (धर्म को) मूँडने और तबाह कर देनेवाली है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात अगर तुम दो आदमियों के सम्बन्ध को बिगाड़ने का प्रयास करोगे तो उन दोनों के तो आपसी सम्बन्ध ही ख़राब होंगे लेकिन इस कृत्य से तुम्हारा अपना धर्म तबाह हो जाएगा।
यह हदीस बताती है कि धर्म वास्तव में चरित्र और व्यक्तित्व का नाम है। जब कोई व्यक्ति बुरा चरित्र और बुरी नीति अपनाता है तो अनिवार्यतः इस स्थिति में उसका धर्म सुरक्षित नहीं रहता। आदमी की बुरी हरकतें और करतूतें हमेशा यही बताती हैं कि वह आदमी धर्म से विमुख हो चुका है।
नाता-रिश्ता तोड़ना
(1) हज़रत मुहम्मद-बिन-ज़ुबैर-बिन-मुतइम (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
"नाते-रिश्ते को तोड़नेवाला स्वर्ग में प्रविष्ट न होगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात नाते-रिश्ते तोड़नेवाले के लिए जो नाते को जोड़ने के बजाए तोड़ता है, स्वर्ग के द्वार बन्द होंगे। वह स्वर्ग में प्रवेश पाने से रह जाएगा।
इससे मालूम हुआ कि नाता-रिश्ता तोड़ना गम्भीर अपराध और गुनाह है। स्वर्ग उन लोगों के लिए नहीं है जिनके हृदय कठोर और प्रेम एवं सौम्यता से रिक्त हों। स्वर्ग तो प्यार-मुहब्बत का घर है। उसमें ऐसे लोग किस प्रकार प्रविष्ट होंगे जो प्रेम के शत्रु हों।
(2) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इबलीस अपना तख़्त पानी पर रखता है फिर अपनी सेना भेजता है। दर्जे में उससे सबसे निकट वह होता है जो उनमें सबसे बढ़कर उपद्रवकारी हो। उनमें से कोई शैतान आकर कहता है कि मैंने अमुक और अमुक कार्य किया है। इबलीस कहता है तुमने कुछ भी न किया। फिर कोई आकर कहता है कि मैंने अमुक व्यक्ति को नहीं छोड़ा (उसके पीछे पड़ा रहा) यहाँ तक कि मैंने उसके और उसकी पत्नी के बीच जुदाई करा दी। इबलीस उसे अपने निकट कर लेता है और कहता है कि हाँ तुमने बड़ा काम किया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि इबलीस का निकटवर्ती वही है और अपनी मानसिकता और मिज़ाज की दृष्टि से वही इबलीस के निकट है जो अधिक से अधिक फ़ितना और फ़साद की बुनियाद डाल सके और लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ सके।
शैतान इबलीस को अपने कार्यों की सूचना देते हैं। उदाहरणस्वरूप कोई कहता है कि मैंने अमुक को शराब पीने पर उभारा और अमुक को चोरी करने पर उकसाया।
इबलीस की दृष्टि में बड़ा कारनामा यह है कि लोगों के आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ दिया जाए। इसी लिए वह अपने कारिन्दे से कहता है कि प्रशंसनीय कारनामा तो तुमने अंजाम दिया कि पति और पत्नी में जुदाई डाल दी। असल और दूरगामी परिणामवाला कार्य तो यह है कि लोगों के आपसी सम्बन्ध और विशेषकर पति और पत्नी के सम्बन्ध में दरार उत्पन्न कर दी जाए। परिवारों को तबाह कर दिया जाए और मानव समाज को उपद्रव और बिगाड़ से भर दिया जाए।
इस हदीस में समाज के ऐसे तत्वों के लिए कड़ी चेतावनी है जिन्हें लोगों के बीच सुधार का काम करने के बजाय उनके सम्बन्धों को बिगाड़ने ही में आनन्द मिलता है और इसी कार्य में वे अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं।
ज्ञान की अवमानना
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिसने वह ज्ञान सीखा जिसके द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है मगर वह उसे इस उद्देश्य से सीखता है कि उसके द्वारा सांसारिक सुख-सुविधा प्राप्त करे तो वह क़ियामत के दिन स्वर्ग की सुगन्ध भी न पा सकेगा।" (हदीस : तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)
व्याख्या : चूँकि उसने उस ज्ञान की अवमानना की और उसने उसे तुच्छ वस्तु की प्राप्ति का साधन बनाया और अपने आप को मूल उद्देश्य से दूर रखा इसलिए वह ईश्वर की प्रसन्नता से वंचित ही रहेगा। स्वर्ग चूँकि ईश्वर की प्रसन्नता और उसकी रज़ामन्दी ही का परिचायक है इसलिए वह स्वर्ग के निकट भी न फटक सकेगा। उसे स्वर्ग तो क्या स्वर्ग की सुगन्ध भी नसीब न हो सकेगी।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जिस व्यक्ति से कोई ऐसी बात पूछी गई जिसका उसे ज्ञान है फिर उसने उसे छिपाया तो क़ियामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी अबू-दाऊद)
व्याख्या : इब्ने-माजा में यह हदीस हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है।
ज्ञान को छिपाए रखना और लोगों को उससे लाभ उठाने का अवसर न देना यहाँ तक कि जो लोग उसके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हों उन्हें भी उससे वंचित रखना इतना बड़ा अपराध है कि क़ियामत के दिन ज्ञान को छिपानेवाले के मुँह में नरकाग्नि की लगाम लगाई जाएगी कि जब दुनिया में सत्य प्रकटीकरण के लिए तेरा मुँह न खुल सका तो अब इसे बन्द ही रहना चाहिए।
मिथ्या-प्रलाप और वाक्पटुता
(1) हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“मैंने समझ लिया है (या यह कहा कि मुझे आदेश हुआ है) कि मेरा भाषण और मेरी बातचीत संक्षिप्त हो, क्योंकि संक्षिप्त भाषण ही अच्छा होता है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “यदि वह संक्षिप्त भाषण देता और मध्यमार्ग का ध्यान रखता तो उसके लिए अच्छा होता।" और अपनी बात के समर्थन में इस हदीस का उल्लेख किया।
आम तौर से लोग अनावश्यक ही लम्बा-चौड़ा भाषण देते और अपनी बात-चीत को तूल देते हैं। सभ्य व्यक्ति इसे कभी पसन्द नहीं कर सकता। लम्बी बात हमेशा उकतानेवाली होती है। इससे एक प्रकार की बेदिली ही पैदा होती है। लोग ऐसे भाषण करनेवालों से खिन्न होने लगते हैं जो लम्बे भाषण करने के अभ्यस्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बातें और उनके भाषण नीरस और प्रभावहीन होकर रह जाते हैं।
संक्षिप्त भाषण जो संग्राहक भी हो उसे लोग ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं और संक्षिप्त बातें याद भी रह जाती हैं और फिर आदमी को उनपर विचार करने का अवसर भी मिलता है। प्रभावी भाषण या बातचीत सदैव संक्षिप्त हुआ करती है। लम्बी-चौड़ी वार्ता अकसर ग़ाफ़िल हृदयों की पैदावार होती है। जिन लोगों के हृदय ग़फ़लत में डूबे हुए होते हैं, जिनको ईश्वर की महानता और उसके प्रताप और उसके सौन्दर्य का एहसास नहीं होता वे अकसर वाक्पटुता के द्वारा उस रिक्तता को भरने का प्रयास करते हैं जो उनके यहाँ पाई जाती है। लेकिन इस उपाय से उनकी कमज़ोरी तो नहीं दूर होती अलबत्ता सम्भव है लोगों में उनके भाषाज्ञान और वाक्पटुता की प्रसिद्धि हो जाए। लेकिन यह तो कोई उद्देश्य न हुआ।
(2) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल) ने कहा—
“लज्जा और मितभाषिता ईमान की दो शाखाएँ हैं और अश्लील और व्यर्थ बकवास कपटाचार की दो शाखाएँ हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : इस हदीस में ईमान और कपटाचार के स्पष्ट लक्षणों का उल्लेख हुआ है। बताया गया कि मोमिन कभी अश्लील और निर्लज्ज नहीं होता। मोमिन लज्जाशील, अच्छी रुचि और निर्मल स्वभाव का होता है। ये गुण उसे इस बात का अवसर ही नहीं देते कि वह लज्जास्पद नीति अपनाए या असन्तुलित बातें मुख से निकाले। उसे यह चिन्ता रहती है कि उसके मुख से कहीं कोई ग़लत बात न निकल जाए या कहीं वह दुर्वचनों या अश्लील शब्दों का उच्चारण न कर बैठे।
इसके अतिरिक्त चूँकि मोमिन का ध्यान मूलतः ईश्वर की महानता और उसके सौन्दर्य और महानता की ओर रहता है। इसलिए भी बातचीत में विनम्रता या विनयशीलता आ जाती है। मोमिन की अभिरुचि ही इसकी अनुमति नहीं देती कि वह व्यर्थ कामों में व्यस्त हो। अतः वह बस आवश्यक बातें ही करता है और वह भी पूर्ण दायित्व और सावधानी से। उसके लिए आनन्द वाक्पटुता में नहीं वरन् ईश-स्मरण में निहित है और उसके समय का बड़ा भाग अपने सुधार और लोगों की सेवा में व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अश्लील शब्दों का उच्चारण तो अलग रहा, वह अपना मंतव्य भी अमर्यादित रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। अलबत्ता जब किसी मोमिन को किसी विषय में दृढ़ विश्वास हो जाता है तो उसे वह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करता है और उस समय इसकी आवयश्यकता नहीं रहती कि वह इस सिलसिले में नम्रता दिखाए।
इसके विपरीत कपटाचारी निर्लज्ज और दुष्भाषी होता है। वह बातों में अतिशयोक्ति और वाक्पटुता दिखाने का प्रयास करता है। वह व्यर्थ और अनर्गल प्रलाप में अत्यन्त दिलेर और निर्भीक दीख पड़ता है।
अनुचित प्रशंसा
(1) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक व्यक्ति को किसी की प्रशंसा करते हुए सुना। वह उसकी प्रशंसा में अतिशयोक्ति से काम ले रहा था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुमने उसे मार डाला या उस व्यक्ति की कमर तोड़ दी।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मतलब यह कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना और वह भी अतिशयोक्ति के साथ, यह वास्तव में उसे हलाकत और तबाही के ख़तरे में डालना है। इसलिए कि अगर वह अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकार में पड़ गया तो यह उसकी नैतिक मृत्यु होगी और नैतिक मृत्यु से बढ़कर किसी हलाकत और तबाही की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
(2) हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता से उल्लेख करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने एक व्यक्ति की चर्चा हुई तो एक दूसरे व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अफ़सोस तुझपर, तूने अपने साथी की गर्दन काट दी।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कई बार ये शब्द दोहराए और फिर कहा, “अगर तुममें से किसी को प्रशंसा करनी ही पड़े तो इस तरह कहे कि मैं ऐसा समझता हूँ। अगर वस्तुतः वह उसे ऐसा ही समझता है (जैसा कि उसने कहा है) और उसका सही जाननेवाला तो अल्लाह ही है और इस स्थिति में भी ईश्वर की ओर से वह किसी के अच्छे होने पर निश्चयात्मक रूप से कोई बात न कहे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : किसी की प्रशंसा करने में विशेष रूप से उसके सम्मुख उसकी प्रशंसा करने में बड़ी आशंकाएँ होती हैं। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि तूने अपने दोस्त और साथी के हक़ में अच्छा नहीं किया। तूने उसे परीक्षा में डाल दिया। हो सकता है कि वह अपनी प्रशंसा सुनकर अपने को महान समझने लग जाए और अपनी वर्तमान हालत पर सन्तुष्ट और अपने सुधार के प्रति निश्चिन्त हो जाए और इस प्रकार उसके लिए आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए।
अगर किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करनी अनिवार्य हो जाए जिसे वह प्रशंसायोग्य समझता है तब भी प्रशंसा करने में कदापि अतिशयोक्ति न करे बल्कि यह कहे कि “जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह ऐसा है।" सत्य क्या है इसे तो परमात्मा ही जानता है। कभी निश्चयात्मक रूप में किसी के विषय में अन्तिम निर्णय न दे। उदाहरणार्थ हम यह न कहें कि अमुक व्यक्ति तो जन्नती या ईश्वर का निकटवर्ती है। ऐसा कहने का अधिकार किसी बन्दे को प्राप्त नहीं है। क्या मालूम जिसे हम जन्नती या ईश्वर का निकटवर्ती ठहरा रहे हैं वह ईश्वर की दृष्टि में क्या है? फिर हमें किसी के बारे में यह भी नहीं मालूम कि उसका अन्त इस्लाम पर होता है या कुफ़्र पर।
सारांश यह कि किसी की प्रशंसा करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और अतिशयोक्ति से बचना चाहिए और यथासम्भव इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी की प्रशंसा उसके मुँह पर कदापि न की जाए।
(3) हज़रत मिक़दाद-बिन-असवद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा:
"जब तुम प्रशंसा करनेवालों को देखो तो उनके मुह में ख़ाक डाल दो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : कुछ विद्वानों की दृष्टि में प्रशंसकों से अभिप्राय यहाँ वे लोग हैं जिनका पेशा ही चापलूसी और अनुचित प्रशंसा और ख़ुशामद होता है। जो गुणगान और चापलूसी में सत्य और असत्य को सर्वथा भूलकर झूठ का तूमार बाँधते हैं और इस चीज़ को स्वार्थसिद्धि का साधन बना रखा होता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके मुँह में ख़ाक डाल दो। अर्थात उनके गुणगान पर कदापि प्रसन्नता व्यक्त न करो और न उन्हें पुरस्कृत करो। उन्हें नाकाम लौटाओ।
यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि कुछ ऐसी हदीसें भी सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद हैं जिनसे किसी के मुँह पर उसकी प्रशंसा करने की वैधता सिद्ध होती है। इससे विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अगर आदमी के फ़ितने में पड़ने का भय न हो और आवश्यकता पड़े तो उसके मुँह पर प्रशंसा की जा सकती है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के किसी प्रिय और प्रशंसनीय कार्य पर प्रशंसा की जाए ताकि इससे उसका उत्साह बढ़े और उसमें सन्मार्ग में आगे बढ़ने का शौक़ पैदा हो और इससे दूसरे लोगों को भी नेक काम करने की प्रेरणा मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
वचन भंग
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वचन भंग करनेवाले के लिए क़ियामत के दिन एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि यह अमुक के बेटे अमुक का वचनभंग है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मतलब यह कि वचनभंग के विषय में क़ियामत के दिन पूरे तौर पर यह एलान कर दिया जाएगा कि वह व्यक्ति वचन भंग करनेवाला और चरित्रहीन है, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित बना फिरता हो। क़ियामत के दिन उसकी रुसवाई में कोई कमी न होगी। उस दिन उसकी रुसवाई और निन्दा की पूरी व्यवस्था दिखाई देगी।
(2) हज़रत ज़ैद-बिन-अरक़म (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब कोई व्यक्ति अपने भाई से वादा करे और उसकी नीयत यह हो कि वह वादे को पूरा करेगा मगर (किसी कारणवश) पूरा न कर सके और निर्धारित समय पर न आ सके तो उसपर कोई गुनाह नहीं।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात अपने भाई से यह वादा करे कि मैं अमुक समय अमुक स्थान पर आऊँगा और उसका इरादा और नीयत यही हो कि वह अपने इस वादे को अनिवार्यतः पूरा करेगा।
चूँकि असल निर्णायक चीज़ नीयत है, अगर उसकी नीयत वादा भंग करने की नहीं है बल्कि किसी विवशता के कारण वह अपना वादा पूरा करने में असमर्थ रहे और निर्धारित समय पर न पहुँच सके तो वह कदापि गुनहगार न होगा।
झूठी क़सम
(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति क़सम खाकर किसी मुसलमान का हक़ मार ले तो अल्लाह ने उसके लिए नरक अनिवार्य और स्वर्ग वर्जित कर दिया है।” एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, यद्यपि वह तनिक-सी चीज़ हो तब भी? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “यद्यपि वह पीलू की एक टहनी ही क्यों न हो।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : यह जो कहा गया कि किसी मुसलमान का हक़ मार ले, मुसलमान की शर्त इसलिए लगाई गई कि मुस्लिम समाज में इस प्रकार के मामले अकसर मुसलमानों ही के साथ पेश आते हैं। अन्यथा मुसलमान ही का नहीं बल्कि ग़ैर-मुस्लिम का माल भी हड़प करना जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता।
क़सम खाकर किसी का हक़ मारना इस बात का स्पष्ट सुबूत है कि न तो हक़ मारनेवाले को ईश्वर की महानता का कुछ ध्यान है और न ही वह अपने भाई के साथ न्याय करना चाहता है। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं। और हम जानते हैं कि आदमी का अपना चरित्र ही है जो उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाता है।
इस हदीस से यह बात भी मालूम हुई कि यह जानने के लिए कि कोई आदमी चरित्र की दृष्टि से कैसा है, इसके लिए किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, बल्कि किसी साधारण चीज़ से भी आदमी के चरित्र को परखा जा सकता है। पीलू की साधारण मिस्वाक (दाँतुन) के सिलसिले में उसने भाई का हक़ मारा। यूँ देखने में तो उसने अपने भाई को कोई बहुत बड़ी हानि नहीं पहुँचाई लेकिन उसने अपनी इस नीति से अपने बारे में जो ख़बर दी वह साधारण कदापि नहीं है। उसने अपनी इस नीति से यह सिद्ध कर दिया कि वह चरित्रहीन और संकीर्णहृदय है।
(2) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तीन आदमी ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन ईश्वर न उनसे बात करेगा, न उनपर कृपादृष्टि डालेगा और न उन्हें उत्कृष्टता प्रदान करेगा। और उनके लिए दुखदायी यातना है।" हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि “ये लोग तो असफल हुए और टोटे में पड़े, ऐ अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अपना तहबन्द हद से नीचे लटकानेवाला, एहसान जतानेवाला और झूठी क़स्में खाकर अपना सौदा चलानेवाला।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : तहबन्द को हद से नीचे लटकाना अहंकार का प्रतीक है। इसी लिए तहबन्द को हद से नीचे लटकानेवाले को असफल कहा गया।
मालूम हुआ कि क़ियामत के दिन, जो ईमानवालों की आशाओं और अभिलाषाओं का दिवस है, ईश्वर ऐसे लोगों से विरक्त होगा। न तो उन्हें ईश्वर से बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, न ईश्वर उनपर कृपादृष्टि डालेगा और न ही उनके व्यक्तित्व को निखारेगा जो अहंकारी और संकीर्णहृदय हैं, जिन्हें झूठी क़स्में खाकर अपना सौदा चलाने में भी कोई संकोच नहीं होता।
(3) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति शासक के आदेश से क़सम खाए और वह अपनी क़सम में झूठा हो और उद्देश्य उसका किसी मुसलमान व्यक्ति का माल मार लेना हो तो वह क़ियामत के दिन अल्लाह से इस हाल में भेंट करेगा कि अल्लाह उसपर क्रुद्ध होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : दुनिया में कोई व्यक्ति झूठी क़स्में खाकर शासक को तो धोखा दे सकता है लेकिन उस सर्वोच्च शासक ईश्वर को कैसे धोखा दे सकेगा जिससे बढ़कर वास्तविकता से कोई दूसरा अवगत नहीं हो सकता। क़ियामत के दिन, जो ईश्वर से मुलाक़ात का दिन है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को अपने से राज़ी और प्रसन्न नहीं पाएगा। उस दिन ईश्वर का प्रकोप ही उसके भाग्य में आएगा।
(4) हज़रत अशअस-बिन-क़ैस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो कोई क़सम खाकर (किसी का) माल मार लेगा वह ईश्वर के सामने कोढ़ी होकर प्रस्तुत होगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : ईश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र उद्देश्य के लिए प्रयोग करना एक ऐसा अपराध है जिसका जितना भी कठोर दंड दिया जाए, न्याय-आधारित ही होगा। कुष्ठ से हरेक को स्वाभाविक रूप से घृणा ही होती है। दुष्चरित्र का अस्तित्व वास्तव में सर्वथा कुष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व घृणास्पद ही हो सकता है। क़ियामत के दिन यह वास्तविकता स्पष्ट होकर रहेगी।
झूठी गवाही
(1) ख़ुरैम-बिन-फ़ातिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो खड़े हो गए और कहा— “झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है।" यह बात आपने तीन बार कही। फिर आपने यह आयत पढ़ी—
“अतः प्रतिमाओं की गन्दगी से बचो और बचो झूठी बात से, इस प्रकार कि अल्लाह ही की ओर के होकर रहो, उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने झूठी गवाही को ईश्वर के साथ साझी ठहराने के समरूप कहा है। और ताकीद के लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी बात को तीन बार दोहराया। और फिर अपनी बात की पुष्टि में सूरा अल-हज्ज की आयत पढ़ी जिसमें झूठ बोलने का उल्लेख शिर्क और मूर्तिपूजा के साथ किया गया है। और दोनों से बचने की ताकीद एक ही शब्द 'इज्तनिबू' अर्थात बचो से की गई है। इससे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तर्क प्रस्तुत किया कि झूठी गवाही अपनी गन्दगी और ईश्वर की अप्रसन्नता का कारण होने की दृष्टि से शिर्क जैसा गुनाह है। झूठी गवाही तो झूठी होती ही है, शिर्क भी झूठ और असत्य होता है। दोनों में सहजातीयता की दृष्टि से बड़ा साम्य (Familiarity) पाया जाता है।
‘जामेअ् तिर्मिज़ी' की एक रिवायत में झूठी गवाही की गणना 'कबाइर' यानी बड़े गुनाहों में की गई है। एक दिन सहाबा से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार कहा—
“क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि सबसे बड़े गुनाह कौन-कौन से हैं?” फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "अल्लाह के साथ साझीदार बनाना, माता-पिता की अवज्ञा करना और मामलों में झूठी गवाही देना और झूठ बोलना।”
अफ़सोस! कि आज झूठी गवाही को लोगों ने एक कला समझ लिया है। उनकी दृष्टि में यह सिरे से कोई बड़ा गुनाह ही नहीं है।
अपराधी की सिफ़ारिश
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना कि—
"जिस किसी की सिफ़ारिश अल्लाह की ओर से निर्धारित दंडों में से किसी दंड के आड़े आए उसने अल्लाह का विरोध किया, और जो व्यक्ति जानते-बूझते नाहक़ बात में झगड़े वह हमेशा ईश्वर के प्रकोप में रहता है जबतक कि उससे रुक न जाए। और जिस किसी ने किसी मोमिन के बारे में ऐसी बात कही जो उसमें न पाई जाए तो अल्लाह उस समय तक उसे नरकवालों के कीचड़ और पीप और लहू में रखेगा जबतक कि वह अपनी कही हुई बात से निकल न आए।” इसे अहमद और अबू-दाऊद ने उद्धृत किया है। बैहक़ी ने शोबिल-ईमान में ये शब्द भी उद्धृत किए हैं, “जो व्यक्ति किसी ऐसे झगड़े में सहयोग दे जिसके सत्य या असत्य होने का ज्ञान उसको नहीं वह उस समय तक ईश्वरीय प्रकोप में घिरा रहेगा जब तक वह उससे बाज़ न आ जाए।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद, अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : जो व्यक्ति आपनी सिफ़ारिश के द्वारा शासक को ईश्वर-निर्धारित दंड देने से रोके उसने ईश्वर का विरोध किया। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी जो यह जानने के बावजूद कि वह जिस बात के लिए झगड़ रहा है वह असत्य और ग़लत है, झगड़ने से बाज़ न आए, ईश्वरीय प्रकोप का भागी होता है।
किसी मोमिन पर कोई मिथ्या दोषारोपण करे और उससे कोई ग़लत बात जोड़कर उसे हानि पहुँचाने का प्रयास करे यद्यपि वह मोमिन उस दोष से मुक्त है और जो बात वह उससे सम्बद्ध कर रहा है वस्तुतः उस मोमिन में नहीं पाई जाती, वह जो कुछ उसके बारे में कहता है मात्र मिथ्यारोपण है।
मूल पाठ में शब्द 'ख़बाल' आया है। ख़बाल वास्तव में उपद्रव को कहते हैं। चाहे यह उपद्रव कर्म में हो या बुद्धि और शरीर में। यहाँ इससे अभिप्राय नरकवालों का ख़ून और पीप आदि गन्दगी है।
यह हदीस बताती है कि ग़लत और अनुचित सिफ़ारिश शरीअत की दृष्टि में किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। ईश्वर-निर्धारित दंडों के क्रियान्वित होने से रोकने का प्रयास वास्तव में ईश्वर का विरोध है। ईश्वर का विरोध करनेवाला अनिवार्यतः ईश्वर का कोपभाजन बनता है। उसके लिए ईश्वरीय प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है कि वह तौबा करे और अनुचित सिफ़ारिश छोड़ दे। एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक मख़्ज़ूमी स्त्री के हाथ काटने का आदेश दिया जिसने चोरी की थी। सहाबा के कहने से जब हज़रत उसामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सिफ़ारिश की बात की तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "तुम ईश्वर-निर्धारित दंडों में से एक दंड के विषय में सिफ़ारिश कर रहे हो!" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) खड़े हुए और सम्बोधित किया—
"तुमसे पहले के लोगों को इसी चीज़ ने हलाक किया कि उनमें कोई शरीफ़ (प्रभावशाली) चोरी करता तो उसे छोड़ देते थे और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उसे दंड देते। ईश्वर की सौगन्ध अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
अपराधी की सिफ़ारिश की भाँति ही झूठ की वकालत करना भी अपने लिए ईश्वरीय प्रकोप को आमन्त्रित करना है। इस अपराध को करनेवाला भी जब तक अपनी नीति को त्याग नहीं देता, ईश्वर का क्रोध उसपर भड़कता ही रहता है। किसी निरपराध मोमिन पर मिथ्यारोपण भी ईश्वर की दृष्टि में अत्यन्त गम्भीर अपराध है। ऐसा व्यक्ति जो किसी निरपराध मुस्लिम और मोमिन की इज़्ज़त से खेलता है और उससे ग़लत बातें जोड़ता है वह वास्तव में अपनी हालत नरकवालों की-सी बना लेता है। उसकी यह नीति अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण होती है। वह देखने में चाहे कितना ही साफ़-सुथरा दिखाई दे लेकिन वास्तव में वह कीचड़, पीप और ख़ून की गन्दगी में गिरा हुआ होता है। और अगर तौबा करके वह अपने को सुधार नहीं लेता तो कोई भी चीज़ उसे उसके बुरे परिणाम से नहीं बचा सकती।
इस हदीस से यह मालूम हुआ कि किसी ऐसे झगड़े में भाग लेना और उसमें सहयोग करना जिसके सत्य और असत्य होने के बारे में आदमी को कुछ भी ज्ञान न हो, एक ऐसी अन्यायपूर्ण नीति है जिसके परिणामस्वरूप ईश्वरीय प्रकोप के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ अपने हिस्से में नहीं आ सकती। इसलिए आदमी को, चाहे मामला कोई भी हो, वह नीति अपनानी चाहिए जो ईश्वर की प्रसन्नता का कारण बने, उसके प्रकोप का नहीं।
हत्या
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि तुम आपस में एक-दूसरे की गर्दनें मारने लगो।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात मेरे बाद कहीं ऐसा न हो कि तुम लोग आपस में लड़ने लगो और द्वेष और शत्रुता यहाँ तक पहुँच जाए कि एक-दूसरे की गर्दन उड़ाने में भी तुम्हें कोई संकोच न हो। तुम अगर आपस में एक-दूसरे पर तलवार उठाओगे तो तुम्हारी यह नीति इस्लाम के विरुद्ध होगी। तुम्हारा यह व्यवहार कुफ़्र होगा या कृतघ्नता। और यह तो अत्यन्त ही गम्भीर बात होगी अगर तुम एक-दूसरे को काफ़िर घोषित कर परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाओ।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जिसने हम पर हथियार उठाया, वह हममें से नहीं है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात उसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं। मैं उससे और उसके इस कृत्य से अत्यन्त विरक्त हूँ। मुसलमानों पर हथियार उठानेवालों को इसकी ख़बर होनी चाहिए कि उनकी यह नीति इस्लामी समाज और उसके अमन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए उन्हें ऐसे क़दम उठाने से पहले इसके दुखद परिणामों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए।
(3) हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना कि—
“जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक-दूसरे के आमने-सामने हों तो हत्यारा और हत दोनों ही नरक में होंगे।" मैंने कहा कि एक तो हत्यारा है किन्तु हत क्यों (नरक में जाएगा)? कहा, "इसलिए कि वह भी अपने साथी की हत्या का इच्छुक था।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात मारा गया व्यक्ति यद्यपि अपने उद्देश्य में सफल न हो सका लेकिन इच्छा और नीयत तो उसकी भी यही थी कि वह अपने भाई को मौत के घाट उतार दे। ईश्वर के यहाँ मूलतः आदमी के इरादे और उसकी नीयत और उसकी भावना को देखा जाता है, फिर उसी के अनुसार उसके बारे में निर्णय किया जाता है।
(4) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“(क़ियामत के दिन) सर्वप्रथम लोगों के उन मुक़द्दमों का निर्णय किया जाएगा जो हत्या से सम्बन्धित होंगे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : हत्या का मामला चूँकि अत्यन्त गम्भीर है इसलिए निर्णय हेतु सर्वप्रथम हत्या के मुक़द्दमे ही पेश होंगे। एक हदीस से मालूम होता है कि सर्वप्रथम क़ियामत के दिन नमाज़ के बारे में पूछा जाएगा। वास्तव में इन दोनों हदीसों में परस्पर कोई विरोध नहीं पाया जाता। हक़ीक़त यह है कि ईश्वर के अधिकारों के सम्बन्ध में सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल होगा वह नमाज़ है। इसलिए ईश्वर के अधिकारों में सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण नमाज़ ही है। लोगों के जो अधिकार हमपर होते हैं उनमें सर्वप्रमुख यह है कि हम उनके हितैषी हों। अब अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या नाहक़ करता है तो उसके बारे में इसके सिवा और क्या कहा जाए कि वह इतना बड़ा अत्याचारी है कि ईश्वर के बन्दों का हक़ अदा करना तो अलग रहा उसे तो दूसरे का अस्तित्व भी गवारा न हुआ। इनसान के सारे हक़ों और अधिकारों का सम्बन्ध उसके जीवन से होता है। नाहक़ क़त्ल से आदमी के सारे हक़ों और अधिकारों का निषेध हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के सारे मामलों और उसके कर्मों का सम्बन्ध उसके जीवन से होता है। जीवन का अन्त कर देने से कर्मों के सारे सिलसिलों का अन्त हो जाता है। हत्या का अर्थ यह होता है कि आदमी की सारी दौड़-धूप और उसकी गतिविधियों का समापन कर दिया जाए। इसलिए नाहक़ हत्या एक गम्भीर अपराध सिद्ध होता है। इसी लिए लोगों के हक़ों और अधिकारों के सिलसिले में सबसे पहले हत्या के विषय में क़त्ल का मुक़द्दमा देखा जाएगा।
(5) हज़रत बरा-बिन-आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सम्पूर्ण संसार की तबाही अल्लाह के निकट एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मुक़ाबले में बहुत हल्की है।" (हदीस : इब्ने-माजा)
व्याख्या : सम्पूर्ण जगत ईश्वर के एक होने और उसके शासनाधिकार और प्रभुता पर गवाह है। वास्तव में विश्व की रचना इसलिए हुई है कि लोग ईश्वर की प्रभुता पर ईमान लाकर उसके आज्ञापालन और दासता को अपनाएँ। यह चीज़ अगर सामने रहे तो इस बात के समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि किसी मोमिन और मुस्लिम बन्दे की हत्या वास्तव में सृष्टि के मूल उद्देश्य के विरुद्ध एक कार्रवाई है। यह एक ऐसा अपराध है जिसकी जघन्यता और गम्भीरता का इससे अधिक प्रभावी वर्णन किसी अन्य उपमा द्वारा सम्भव नहीं जो उपमा इस हदीस में दी गई है।
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“उस सत्ता की सौगन्ध जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं : लोगों पर एक ऐसा समय आएगा कि न हत्यारे को मालूम होगा कि उसने क्यों हत्या की और न मारे गए व्यक्ति को ख़बर होगी कि उसकी हत्या क्यों की गई।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ऐसा उपद्रव और बिगाड़ उत्पन्न होगा कि अन्धाधुन्ध हत्याओं की घटनाएँ घटेंगी। नाहक़ क़त्ल एक आम बात हो जाएगी। इनसानों का रक्त इतना सस्ता हो जाएगा कि हत्या और रक्तपात की घटनाओं पर किसी को कोई आश्चर्य न होगा।
(7) हज़रत अबू-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत से कुछ दिनों पहले ज्ञान उठा लिया जाएगा और अज्ञान फैल जाएगा और 'हर्ज' की बहुतायत हो जाएगी।” और हर्ज से अभिप्राय हत्या है। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात निकृष्टतम प्रकार के लोग धरती में रह जाएँगे। आसमान के नीचे जिनकी हैसियत बदनुमा दाग़ से अधिक न होगी। अज्ञान और अत्याचार का बोलबाला होगा। फिर क़ियामत के घटित होने में कुछ अधिक विलम्ब न होगा।
(8) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब तक कि कोई मोमिन हराम (प्रतिष्ठित) ख़ून बहाने (अकारण हत्या) का अपराधी न हो वह सदैव अपने धर्म की असंकीर्णता से लाभान्वित होता रहता है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : सत्य धर्म तो अवतरित ही इसलिए हुआ है कि लोगों के लिए आसानी और कुशादगी पैदा की जाए और उनको उन जकड़बन्दियों और तंगियों से मुक्ति दिलाई जाए जिनमें चालाक लोग साधारणतः जनता को ग्रस्त रखते हैं। सत्यधर्म का अनुयायी वास्तव में ईश्वर की असीम दयादृष्टि में होता है। उसपर ईश्वर की विशेष अनुकम्पाएँ होती हैं। वह अच्छी आशाओं के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ग़लत क़दम उठाता है और विशेषकर जब वह किसी की नाहक़ हत्या कर देता है तो फिर इस अवैध कर्म के परिणामस्वरूप वह तंगी में पड़ जाता है। प्रत्येक ओर से वह ख़तरों और अन्देशों में गिरफ़्तार दिखाई देता है। वह उस दंड का भागी हो जाता है जो शरीअत ने हत्या के लिए निर्धारित की है। वह अपनी पोज़ीशन इतनी बिगाड़ लेता है कि वह उन लोगों की श्रेणी में आ जाता है जो ईश्वरीय अनुकम्पा से वंचित और निराश होते हैं।
चोरी
(1) हज़रत उबादा-बिन-सामित (रज़ियल्लाहु अन्हु) उल्लेख करते हैं कि मैंने एक जमाअत (कुछ लोगों) के साथ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से 'बैअ्त' (प्रतिज्ञा) की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं तुमसे इसपर बैअ्त लेता हूँ कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, और न चोरी करोगे और न अपनी सन्तान की हत्या करोगे, और न कोई मिथ्या दोषारोपण करोगे जिसे अपने हाथों और पावों के मध्य घड़ लो। और न भले कामों में मेरी अवज्ञा करोगे। तुममें से जिस किसी ने अपना वादा पूरा किया तो उसका प्रतिदान अल्लाह के ज़िम्मे है। और जो व्यक्ति इनमें से कोई अपराध कर बैठे और दुनिया में उसे दण्ड दे दिया गया तो वह उसके लिए प्रायश्चित है और पवित्रता का साधन भी। और जिस किसी के ऐब को अल्लाह ने छिपाया तो फिर मामला अल्लाह के हवाले है। यदि वह चाहे तो उसे दण्ड दे और चाहे तो उसे क्षमा कर दे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : निराधार दोषारोपण करने को अपने हाथों और पैरों के मध्य दोषारोपण कहा है।
जो बैअ्त आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ली वह क़ुरआन की शिक्षा के अनुसार ली। क़ुरआन में है—
“ऐ नबी जब तुम्हारे पास ईमानवाली स्त्रियाँ आकर तुमसे इसपर बैअ्त करें कि वे अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी नहीं ठहराएँगी और न चोरी करेंगी और न व्यभिचार करेंगी और न अपनी औलाद की हत्या करेंगी और न अपने हाथों और पैरों के बीच कोई आरोप घड़कर लाएँगी, और न किसी भले काम में तुम्हारी अवज्ञा करेंगी, तो उनसे बैअ्त ले लो और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यन्त दयावान है।" (60:12)
गुनाह का जो दण्ड दुनिया में किसी को दिया गया उससे उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा और उसे पवित्रता नसीब होगी।
जिस किसी का जुर्म दुनिया में छिपा रह गया, और उसे दुनिया में अपने अपराध का दण्ड नहीं मिला तो किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि आख़िरत में उसे अनिवार्यतः दण्ड मिलेगा ही। यह ईश्वर के अधिकार में है। वह दण्ड भी दे सकता है और उसके पाप को क्षमा भी कर सकता है। इसकी पूरी सम्भावना है कि जिस व्यक्ति ने सच्चे दिल से तौबा करके दुनिया में अपना सुधार कर लिया हो और ईश्वर का आज्ञाकारी बन्दा बनकर संसार से विदा हुआ हो, ईश्वर आख़िरत में भी उसके ऐब छिपाए और उसे कोई दण्ड न दे। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के ऐबपोशी के बावजूद बुरे का बुरा ही बना रहा, वह चाहे दुनिया में दण्ड पाने से बच जाए लेकिन आख़िरत में उसे ईश्वर की पकड़ से बचानेवाली कोई चीज़ न होगी।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“व्यभिचार करनेवाला जिस समय व्यभिचार करता है वह मोमिन नहीं होता और चोर जिस समय चोरी करता है वह मोमिन नहीं होता और शराबी जब शराब पीता है तो वह मोमिन नहीं होता और तौबा स्वीकृत होगी उसके बाद।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात वह मोमिन के चरित्र से दूर या परे होता है। नैतिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति वह कार्यशैली अपनाता है जो उसके ईमान की अपेक्षाओं के विरुद्ध हो तो इसका अर्थ इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति ऐसा मोमिन नहीं रहा जिसका ईमान हृदय के किसी कोने में छिपा नहीं रहता वरन् जिसका पूरा जीवन उसके ईमान के प्रभाव में रहता है और प्रत्येक छोटी-बड़ी परिस्थिति में उसके ईमान के स्पष्ट प्रभाव देखे जा सकते हैं।
इस हदीस का अर्थ यह नहीं है कि व्यभिचार, चोरी और मदिरापान ही ऐसे गुनाह हैं जिनके करने से आदमी मोमिन के चरित्र से दूर हो जाता है बल्कि उसके दूसरे गुनाह भी इस बात का प्रमाण होते हैं कि आदमी मोमिन के गुणों से वंचित है। इन तीन बड़े गुनाहों से वास्तव में तमाम ही गुनाहों का, जो इनसान कर सकता है, प्रतिनिधित्व होता है। व्यभिचार उन समस्त गुनाहों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका सम्बन्ध मनेच्छाओं और वासनाओं से होता है। लोभ-लिप्सा के कारण आदमी जिन गुनाहों में पड़ता है उन गुनाहों का प्रतिनिधित्व चोरी से होता है। ठीक इसी प्रकार मदिरापान से उन गुनाहों का प्रतिनिधित्व होता है जो आदमी को ईश्वर की याद से रोकते और उससे ग़ाफ़िल कर देते हैं और वह इससे बेख़बर हो जाता है कि ईश्वर के स्मरण में जो आनन्द और मस्ती है वह किसी और चीज़ में नहीं है।
(3) हज़रत अदी-बिन-उमैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी को हम आमिल (हाकिम) नियुक्त करें और कुछ काम लें और वह हमसे एक सूई या उससे बढ़कर कोई तुच्छ वस्तु छिपा रखे तो यह भी चोरी है। वह क़ियामत के दिन उसको लिए हुए उपस्थित होगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि प्रमुख या अमीर की आज्ञा के बिना सूई के बराबर भी कोई चीज़ अपने प्रयोग में लाना चोरी है। क़ियामत के दिन ऐसी चोरी भी आदमी के अपयश का कारण बनेगी।
(4) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है—
“जिस किसी को भोजन का निमन्त्रण दिया जाए और वह उस निमन्त्रण को स्वीकार न करे तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा की। और जो व्यक्ति बिना बुलाए भोज में उपस्थित हुआ तो वह चोर बनकर भोज में उपस्थित हुआ और लूट-मार कर निकला।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : बिना किसी विशेष मजबूरी के और उचित कारण के किसी की दावत को अस्वीकृत करना इस्लामी स्वभाव के प्रतिकूल है। इस्लाम एक ऐसे समाज का निर्माण चाहता है जिसके लोगों में एकात्मता और प्रेम का वातावरण पाया जाता हो। अपने भाई के निमन्त्रण को ठुकरा देना ऐसी नीति नहीं है जिससे दिलों की दूरियाँ कम हों और इस्लामी समाज की सुदृढ़ता में मदद मिल सके।
बिना बुलाए किसी के यहाँ भोज में सम्मिलित होना अत्यन्त घिनावना काम है। यह एक निकृष्टतम प्रकार की चोरी और डकैती है।
किसी की नक़ल उतारना
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं इसे हरगिज़ पसंद नहीं करता कि किसी व्यक्ति की नक़ल उतारूँ, यद्यपि मेरे लिए ऐसा और ऐसा ही क्यों न हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : किसी व्यक्ति की नक़ल उतारना चाहे उसका सम्बन्ध मुख से हो या व्यवहार से, दोनों ही अवैध हैं और परनिन्दा में आते हैं, जो अत्यन्त निकृष्ट कर्म है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन कि “मेरे लिए ऐसा और ऐसा ही क्यों न हो।" इससे अभिप्रेत यह है कि कोई चाहे मुझे कितनी ही धन-सम्पत्ति दे, मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं हो सकता कि मैं किसी के दोषों को प्रकट करूँ। इससे मालूम हुआ कि इस प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म हरकत भी किसी के लिए शोभनीय नहीं है। इस प्रकार की हरकत मनुष्य की गरिमा के प्रतिकूल है। इससे अगर किसी के ऐब खुलते हों तो फिर तो यह और अधिक बुरा होगा। इस प्रकार के कृत्यों से स्वयं आदमी का अपना व्यक्तित्व इतना आहत होता है कि उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन-सम्पत्ति और सांसारिक लाभ के द्वारा नहीं हो सकती।
पुष्टि के बिना किसी बात को फैलाना
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"आदमी को गुनाह के लिए यही पर्याप्त है कि जो कुछ सुने उसे बयान करता फिरे।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : किसी बात की पुष्टि के बिना लोगों में उसकी चर्चा करना और उसे फैलाना भी झूठ का प्रसार है, और झूठ के गुनाह होने में किसे सन्देह हो सकता है। इसी लिए हदीस में कहा गया—
“आदमी को झूठ के लिए यही पर्याप्त है कि वह जो कुछ सुने उसे बयान करता फिरे।"
कभी-कभी पुष्टि के बिना बात फैलाने का परिणाम अत्यन्त दुखद रूप में सामने आता है। आप जानते हैं कि कितने ही उपद्रव मात्र अफ़वाहों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। कितने ही बेगुनाह लोगों के हताहत होने के पीछे मात्र अफ़वाहें काम कर रही होती हैं जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं होता। निराधार अफ़वाहों और ग़लत ख़बरों के कारण वातावरण में तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम रक्तपात, तबाही और बरबादी के सिवा कुछ नहीं होता।
बदनिगाही
(1) हज़रत बुरीदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ अली, (किसी अजनबी स्त्री पर) दोबारा दृष्टि न डालना, पहली दृष्टि तो तुम्हारी है, दूसरी तुम्हारी नहीं है।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात प्रथम दृष्टि तो क्षम्य है क्योंकि इसमें तुम्हारी नीयत और इरादा शामिल नहीं होता लेकिन दोबारा दृष्टि डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह दूसरी दृष्टि तुम्हारी नहीं, शैतान की है। इसमें मन की इच्छा शामिल हो जाएगी। किसी पराई स्त्री के सौन्दर्य पर दृष्टि डालना और उससे रस लेना अत्यन्त नाज़ुक मामला है। वह स्त्री तुम्हारे लिए नहीं अपने पति के लिए है। पराई चीज़ का रसास्वादन न केवल यह कि एक प्रकार की चोरी और विश्वासघात है, बल्कि इसका दण्ड भी आदमी को संसार ही में मिल जाता है। इस अनुचित कृत्य से हृदय की पवित्रता शेष नहीं रहती। और इसकी बड़ी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि वह किसी फ़ितने में पड़कर अपनी प्रतिष्ठा और शान्ति दोनों गँवा बैठे।
(2) हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से (अजनबी औरत पर) सहसा नज़र पड़ जाने के विषय में पूछा तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— "तुम अपनी नज़र फेर लो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात नज़र जमाए न रहो बल्कि तुरन्त अपनी दृष्टि हटा लो।
रिश्वत
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने रिश्वत देने और रिश्वत लेनेवाले दोनों पर लानत की है। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : बैहक़ी ने शोबिल-ईमान में यह हदीस हज़रत सौबान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उद्धृत की है और इसमें शब्द 'राइश' भी आया है। अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस व्यक्ति पर भी लानत की है जो रिश्वत लेनेवाले के बीच सम्पर्क या साधन बनता हो। जिस किसी पर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने लानत की हो उसके दुर्भाग्य में क्या सन्देह हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की फिटकार पड़ेगी और वह ईश्वरीय अनुकम्पाओं से वंचित होगा सिवाय इसके कि वह तौबा करके अपना सुधार कर ले।
(2) हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना—
“जिस किसी क़ौम में व्यभिचार की बहुतायत हो जाती है, अनिवार्यतः वह अकालग्रस्त हो जाती है। और जिस किसी क़ौम में रिश्वत आम हो जाती है, वह अनिवार्य रूप से भयाक्रांत हो जाती है।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : व्यभिचार और रिश्वतख़ोरी क़ानूनी अपराध के अतिरिक्त नैतिक रूप से भी ऐसे घिनावने क़िस्म के गुनाह और निकृष्टतम कृत्य हैं कि आख़िरत के दण्ड के अतिरिक्त दुनिया में भी उनका वबाल विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अतएव इस हदीस में रिश्वत की एक नहूसत यह बयान की गई है कि इसके आम होने की स्थिति में क़ौम पर भय और दहशत छाकर रहती है। रिश्वत देने और लेनेवाली क़ौम में ऐसा कायर स्वभाव पैदा हो जाता है कि उसमें वीरता, साहस, उच्च उत्साह, पौरुष आदि नैतिक गुण शेष नहीं रहते। फिर यह क़ौम अपने लोगों से भी भयभीत रहती है और अन्य क़ौमों का भय भी उसपर छाया रहता है। रिश्वतख़ोर शासक अपने दायित्वों का निर्वाह करने में हमेशा कोताह पाए गए हैं। उनकी इस आपराधिक नीति के कारण पुरुषार्थ और पौरुष की आशा उनसे नहीं की जा सकती। अन्तरात्मा और न्यायप्रियता की निधि से वंचित व्यक्ति में वह उर्जा और उत्साह कहाँ से आ सकता है जिसके कारण उसे अपनी महानता और मर्यादा का लिहाज़ हो सकता। ऐसे लोग स्वयं अधमता का जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी क़ौम को भी अधमता में ग्रसित रखते हैं। इसे भूलना नहीं चाहिए कि जो क़ौम त्याग और उत्सर्गभाव से वंचित हो चुकी हो तो भय, अधमता और अपमान उसकी नियती बन जाती है।
हक़ मारना
(1) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मज़लूम की फ़रियाद और पुकार से बचते रहो, क्योंकि वह प्रतापवान ईश्वर से केवल अपना हक़ माँगता है और अल्लाह किसी हक़दार को उसके अपने हक़ से रोकता नहीं।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : अन्याय और अत्याचार किसी भी तरह जाइज़ नहीं। इसी लिए कहा गया कि किसी पर अत्याचार न करो कि वह ईश्वर से फ़रियाद करने पर विवश हो जाए और तुम्हारे हक़ में बददुआ करे। ईश्वर किसी का हक़ नहीं रोकता। मज़लूम की फ़रियाद व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए ईश्वर के प्रकोप और उसकी पकड़ से बचो और अत्याचार और किसी का हक़ मारने से हमेशा बचते रहो।
जब्र और ज़्यादती
(1) हज़रत वायल-बिन-हुज्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति किसी की ज़मीन अत्याचारी बनकर छीन लेगा वह (क़ियामत के दिन) अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उसपर अत्यन्त क्रुद्ध होगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात कोई यह न समझे कि अत्याचारपूर्ण नीति अपनाकर यदि वह किसी व्यक्ति की भूमि या और कोई वस्तु छीन लेता है तो वह अपने लिए अच्छा करता है। किसी की चीज़ चाहे उसके क़ब्ज़े में आ गई हो तो उसने अपने इस कार्य से ईश्वर और उसकी अनुकम्पाओं से स्वयं को वंचित कर लिया। अगर आज नहीं तो क़ियामत के दिन उसे भलीभाँति मालूम हो जाएगा कि वास्तव में उसने क्या खोया है और क्या पाया है। मंज़िल पर पहुँचने के बाद वह देखेगा कि ईश्वर के प्रतिदानों और उसकी अनुकम्पाओं के बजाय उसे ईश्वर के प्रकोप ही का सामना करना पड़ रहा है। काश! मानव इस दुर्गति से दोचार होने से पहले ही इस सत्य को जान सकता और उसका जीवन हर प्रकार की उच्छृंखलता और अत्याचारपूर्ण नीति से सर्वथा मुक्त हो सकता।
(2) हज़रत सईद-बिन-ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जिस किसी व्यक्ति ने अत्याचारपूर्ण तरीक़े से किसी की भूमि हथिया ली, क़ियामत के दिन उसके गले में सातों धरतियों का तौक़ पहना दिया जाएगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : ज़बरदस्ती किसी से किसी की कोई चीज़ छीन लेना ऐसा सामाजिक और नैतिक अपराध है कि शरीअत ने इसके लिए कठोर से कठोर दंड निर्धारित किया है। किसी की सम्पत्ति को हड़प लेना और अनुचित रूप से किसी वस्तु का अतिक्रमण कर लेना कितना गम्भीर अपराध है इसका अनुमान इस हदीस से भलीभाँति किया जा सकता है।
जिस व्यक्ति ने भूमि के एक टुकड़े के लिए अत्याचार किया तो सातों धरतियाँ उसके गले का तौक़ बना दी जाएँगी। अर्थ यह है कि भूमि के लोभ में उसने अत्याचार और द्रोहपूर्ण नीति अपनाई, क़ियामत में वही लोभ उसके लिए एक विपत्ति और संकट सिद्ध होगा। शरहुस्सुन्नह में गले में धरतियों का तौक़ डाले जाने का अर्थ यह बताया गया है कि भूमि का अतिक्रमण करनेवाले व्यक्ति को ईश्वर धरती में धँसा देगा और धरती उसकी गर्दन को इस प्रकार जकड़ लेगी मानो उसकी गर्दन तौक़ से जकड़ दी गई हो।
(3)
गिरावट और पस्ती
पक्षपात
(1) फ़लस्तीन निवासी उबादा-बिन-कसीर शामी अपने क़बीले की एक स्त्री फ़सैला के माध्यम से रिवायत करते हैं कि उसका वर्णन है कि मैंने अपने पिता को यह कहते हुए सुना कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा कि क्या यह भी पक्षपात है कि कोई व्यक्ति अपनी क़ौम से प्रेम करे? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“नहीं, बल्कि पक्षपात यह है कि कोई व्यक्ति अपनी क़ौम की सहायता उस स्थिति में भी करे जबकि वह अत्याचार कर रही हो।” (हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा)
व्याख्या : मालूम हुआ कि अपने समुदाय या गरोह से प्रेम या उसके अधिकारों या हितों की प्राप्ति या रक्षा का ऐसा प्रयास जिससे दूसरों के जायज़ अधिकारों या हितों को हानि न पहुँचे, पक्षपात नहीं है। अलबत्ता अपनी क़ौम का ऐसा समर्थन जिसमें दूसरों से अनुचित द्वेष और घृणा की भावनाएँ प्रबल हों या अपने समुदाय के किसी ऐसे संघर्ष में सहयोग जो स्पष्टतः अत्याचार और अतिवादिता पर आधारित हो, इसे अज्ञानपूर्ण पक्षपात के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। इस्लाम इस प्रकार के पक्षपात को मिटाने के लिए ही आया है। इसलिए कि अज्ञानपूर्ण पूर्वाग्रह और पक्षपात के साथ किसी उच्च धारणा और विचार और किसी श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस्लाम एक वैश्विक दृष्टिकोण और विचारधारा है। वह कभी भी किसी संकीर्णता और साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं कर सकता।
(2) हज़रत मअरूर-बिन-सुवैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि हम अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास रबज़ा में गए। वे एक चादर ओढ़े हुए थे और उनके ग़ुलाम ने भी उसी प्रकार की चादर ओढ़ रखी थी। हमने कहा कि ऐ अबू-ज़र, यदि तुम ये दोनों चादरें ले लेते तो एक पोशाक बन जाती। इसपर उन्होंने कहा कि मुझमें और मेरे एक भाई में कुछ तेज़ बातें हो गईं। उसकी माँ अरब न थी (बल्कि अजमी थी), मैंने उसे उसकी माँ का ताना दिया। उस व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मेरी शिकायत कर दी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मेरी भेंट हुई तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ अबू-ज़र! तुझमें अज्ञान मौजूद है।" मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जो कोई व्यक्ति लोगों को गाली देगा तो वे उसके माता-पिता को गाली देंगे। आपने कहा, “ऐ अबू-ज़र, तुझमें अज्ञान मौजूद है। वे तुम्हारे भाई हैं। ईश्वर ने उनको तुम्हारे अधीन किया है तो तुम उनको वही खिलाओ जो स्वयं खाते हो और वही पहनाओ जो स्वयं पहनते हो और उनसे उनकी सामर्थ्य से बढ़कर काम न लो, और अगर ऐसा कोई काम उनसे लो तो फिर उसमें उनका हाथ बटाओ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : रबज़ा एक स्थान का नाम है।
इस हदीस से मालूम होता है कि वह व्यक्ति, जिसको हज़रत अबू-ज़र भाई कह रहे हैं, ग़ुलाम था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मातहतों और ग़ुलामों को भाई कहा है। इसलिए हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी उसे भाई कह रहे हैं।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन का कि ऐ अबू-ज़र तुझमें अज्ञान मौजूद है, अर्थ यह है कि अभी तुझमें अज्ञानकाल का कुछ न कुछ प्रभाव शेष है। अपने वंश पर गर्व करना और दूसरों के माँ-बाप विशेष रूप से अगर वे ग़ैर-अरब हों, तुच्छ समझना यह अज्ञानकाल की चीज़ है। इसका इस्लाम से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता।
हदीस की किताब 'मुस्लिम' ही की एक रिवायत में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जब कहा कि “अबू-ज़र, तुझमें अज्ञान मौजूद है" तो हज़रत अबू-ज़र ने कहा, इस बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी (मुझमें अज्ञान शेष है?) आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "हाँ।”
कोई किसी को बुरा कहे तो अधिक से अधिक यह हो सकता है कि बुरा कहनेवाले को भी बुरा कह दिया जाए। यह कदापि उचित नहीं हो सकता कि उसके माता-पिता को बुरा कहा जाए जिनका कोई दोष नहीं। ग़ुलाम जो तुम्हारे अधीन होते हैं उनके साथ तुम्हारा सुलूक अच्छे-से-अच्छा होना चाहिए। तुम्हें उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। वे कोई पराए नहीं, तुम्हारे भाई हैं। उनसे काम उनकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लो। और अगर कोई ऐसा काम लेना पड़ जाए जो उनकी सामर्थ्य से बाहर हो तो इस काम में उनका हाथ बटाओ ताकि वे परेशानी में न पड़ें।
निर्लज्जता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरी पूरी उम्मत निश्चिन्तता की दशा में है सिवाय उन लोगों के जो अपने अवगुणों और गुनाहों को उजागर करते हैं। और यह बात कितनी संवेदनहीनता और बेपरवाही की है कि कोई व्यक्ति रात में कोई बुरा कर्म करे और प्रातः जबकि अल्लाह ने उसे छिपा लिया था वह लोगों से कहता फिरे कि ऐ अमुक, मैंने रात को ऐसा और ऐसा अपकर्म किया हालाँकि उसके प्रभु ने रात में उसके ऐब को छिपाया था और उसने प्रातः ही अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात लोगों के लिए इसकी सम्भावना है कि ईश्वर दुनिया ही में नहीं आख़िरत में भी उनके ऐबों को छिपाए। उनको तौबा का अवसर मिले और उनका सुधार हो सके और वे बदनामी से सुरक्षित रहें। लेकिन जो लोग इतने अधिक निर्भय और निर्लज्ज हों कि उन्हें अपनी बदनामी की कोई चिन्ता ही न हो, खुल्लम-खुल्ला और अत्यन्त ढिठाई से गुनाह करते रहें और कोई शर्म उनके आड़े न आए, वे अपने गुनाहों और कुकृत्यों की इस प्रकार चर्चा करते फिरें मानो उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो, ऐसे लोग दुनिया में भी अपमानित होते हैं और आख़िरत में भी उनसे कड़ी पूछताछ होगी। वे ईश्वर की पकड़ से अपने आप को बचा नहीं सकते। दुनिया में लोग उन्हें अच्छे शब्दों से कभी याद नहीं कर सकते। विद्वानों की दृष्टि में भी ऐसे मर्यादाहीन और खुल्लम-खुल्ला गुनाहों में ग्रस्त व्यक्ति की निंदा कोई निंदा नहीं है। आख़िरत में भी रुसवाई ही उनके हिस्से में आएगी।
(2) हज़रत अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन अल्लाह की दृष्टि में सबसे बड़ी अमानत, और एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन दर्जे के लिहाज़ से अल्लाह की दृष्टि में सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा जो अपनी पत्नी से सम्भोग करे और उसकी पत्नी उससे सम्भोग करे और फिर वह उसके रहस्य की चर्चा करता फिरे।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : पति और पत्नी के मध्य जो प्रेम और राज़ की बातें होती हैं और उनके मध्य यौन सम्बन्धी जो बातें पेश आती हैं उनकी हैसियत एक बड़ी अमानत की है। प्रत्येक पति का दायित्व है कि वह इस अमानत की रक्षा करे। अगर कोई पति इस अमानत का लिहाज़ नहीं रखता बल्कि उसके और उसकी पत्नी के बीच जो कुछ प्रेमपूर्ण वार्तालाप और यौन सम्बन्धी बातें होती हैं वह उनकी चर्चा लोगों में करता फिरता है, उससे क़ियामत के दिन कड़ी पूछताछ होगी। पति और पत्नी के मध्य जो व्यक्तिगत और यौन मामलों से सम्बन्धित बातें होती हैं, उनको दूसरों के सामने बयान करना नैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि शरीअत की दृष्टि से भी अत्यन्त बुरा है।
जाहिलीयत का आमन्त्रण
(1) हज़रत जुन्दुब-बिन-अब्दुल्लाह बजली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति अन्धे झंडे के तले मारा जाए इस हाल में कि वह पक्षपात का आमन्त्रण देता हो या पक्षपात का समर्थन करता हो तो वह जाहिलीयत में मारा गया।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : जो व्यक्ति सत्य-असत्य कुछ न समझता हो, जिसके लिए जाहिली दुराग्रह और अपनी क़ौम और अपना गरोह ही सब कुछ हो, अपनी क़ौम और अपने सम्प्रदाय के पक्षपात और अनुचित समर्थन में न वह न्याय का ध्यान रखता हो और न उसकी दृष्टि में नैतिकता और सज्जनता कोई चीज़ हो, जिसकी दृष्टि में वैध और उचित वह हो जिसको उसकी क़ौम वैध और उचित ठहराती हो चाहे वह अत्याचार और अन्याय ही क्यों न हो। और अनुचित वह हो जिसको उसकी क़ौम अनुचित घोषित करे चाहे वह सत्य और न्याय और उदारता ही क्यों न हो और वह उसी जाहिली पक्षपात का आमन्त्रणदाता हो और उसी जाहिलीयत का समर्थक बनकर खड़ा हो, ज़ाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को अज्ञान और अन्धकार का ही ध्वजावाहक कहा जा सकता है। अब अगर वह अपने अन्धे झंडे के तले पक्षपात के लिए लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसकी मृत्यु सत्य के मार्ग में नहीं बल्कि अज्ञान के मार्ग में होगी।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“जो व्यक्ति अपना हाथ आज्ञापालन से खींच ले वह क़ियामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके पास कोई तर्क न होगा। और जिस व्यक्ति की मृत्यु इस हाल में आए कि उसने बैअ्त न की हो, उसकी मृत्यु जाहिलीयत की मृत्यु होगी।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस्लाम में सामूहिकता को मौलिक महत्व प्राप्त है। सामूहिक व्यवस्था के बिना इस्लामी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। शान्ति स्थापना और इस्लाम की समस्त बरकतों और मुस्लिम समुदाय की शक्ति का रहस्य इस्लामी शासन व्यवस्था की सुदृढ़ता में निहित है। अब अगर कोई व्यक्ति इस्लामी राज्य के प्रमुख के आज्ञापालन से विमुख होता है तो वास्तव में वह उस इमारत को ढाने पर आमादा है जिसका निर्माण और सुदृढ़ता दोनों ही इस्लाम में अभीष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति अपने इस अपराध के पक्ष में ईश्वर के सामने कोई तर्क प्रस्तुत न कर सकेगा। ईश्वर के यहाँ उसकी हैसियत एक अपराधी ही की हो सकती है और वहाँ कोई भी न होगा जो उसे उसके अपराध के दंड से मुक्ति दिला सके।
इस्लामी जीवन अपनाने का अर्थ यह होता है कि आदमी सामूहिक व्यवस्था को स्वीकार करे और उससे फ़रार इख़्तियार न करे। मुस्लिम समुदाय का यह दायित्व है कि अगर उसका कोई अमीर न हो तो वह पहली फ़ुर्सत में अपना कोई अमीर निर्वाचित करे और उसके नेतृत्व में अपनी सामूहिकता का निर्माण करे। उसके समस्त मामले और विशेषकर सामूहिक मामले अमीर के नेतृत्व और निर्देशन ही में निर्णित हों। ईश्वर संसार में मुस्लिम समुदाय को प्रभावी देखना चाहता है। दुनिया में शक्ति और सुदृढ़ता के लिए सामूहिक व्यवस्था की स्थापना अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त उस महान और उच्च उद्देश्य की प्राप्ति भी सामूहिक व्यवस्था के बिना सम्भव नहीं जिसके लिए इस समुदाय को अस्तित्व में लाया गया है। उच्च और श्रेष्ठ उद्देश्य से अभिप्राय है दमन और अत्याचार का अन्त और सत्यधर्म की स्थापना।
धोखाधड़ी और बात से फिर जाना
(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
"प्रत्येक ग़द्दार के लिए एक झंडा होगा जो उसकी धोखाधड़ी और विश्वासघात का प्रतीक होगा।" (हदीस : बुख़ारी)
(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"जब अल्लाह क़ियामत के दिन सब अगलों और पिछलों को एकत्र करेगा तो हरेक बेवफ़ा और वचनभंग करनेवाले का एक झंडा ऊँचा किया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि यह अमुक के बेटे अमुक का वचनभंग है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अरब की परम्परा थी कि किसी चीज़ को प्रचारित करने के लिए बाज़ार में झंडा खड़ा करते थे। क़ियामत के दिन दग़ाबाज़ और वचनभंग करनेवाले के अनावरण और सबके सामने उसे अपमानित करने के लिए झंडा बुलन्द किया जाएगा ताकि वह खुली आँखों से अपनी प्रतिष्ठा को ख़ाक में मिलते हुए देख सके। लोग जान लें कि अमुक व्यक्ति अत्यन्त ही नीच और अधम है, दुनिया की ज़िन्दगी में दग़ाबाज़ी और विश्वासघात उसका पेशा रहा है।
(3) हज़रत अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“हरेक वचनभंग करनेवाले के लिए क़ियामत के दिन एक झंडा होगा जो उसके वचनभंग के अनुपात से ऊँचा किया जाएगा, और जान लो कि उससे बड़ा वचनभंजक कोई नहीं जो आम लोगों का शासक होकर वचनभंग करे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि क़ियामत के दिन आदमी का वचनभंग और धोखाधड़ी उसके लिए केवल अपयश का कारण होगा। जो आज जितना बड़ा वचनभंजक है क़ियामत के दिन उसे उतने ही अधिक अपमान का सामना करना पड़ेगा।
यह हदीस यह भी बताती है कि दुनिया में सबसे बड़ा वचनभंग, शासक और नेता का वचनभंग है। शासक का दायित्व है कि वह स्वयं न्याय पर क़ायम रहे और लोगों को न्याय पर क़ायम रखने के लिए प्रयासरत हो। अब अगर वह इस दायित्व को भूलकर लोगों के प्राणों और सम्पत्तियों पर अत्याचार करता और उनके अधिकारों का हनन करता है तो उससे बड़ा वचनभंजक कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी सामान्य व्यक्ति के वचनभंग की तुलना उसके वचनभंग से कदापि नहीं की जा सकती। शासक के वचनभंग से किसी एक को नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जनता को हानि पहुँच सकती है। इसलिए सब लोगों से बढ़कर अपमान उसी के भाग्य में आएगा। अमीर या शासक का विश्वासघाती या वचनभंजक होना जघन्य अत्याचार है। लोगों के साथ उसके वचनभंग का अर्थ यह होता है कि वह उनकी उचित आशाओं को पूरा न करे और जनता का शासक के साथ वचनभंग यह है कि वह बैअ्त को अनधिकृत रूप से तोड़ दे और बिना किसी शरई उज़्र (औचित्य) के शासक के साथ सहयोग न करे और उसके आज्ञापालन से मुख मोड़ ले।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"प्रतापवान ईश्वर का कथन है कि तीन व्यक्ति ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन मैं उनका शत्रु हूँगा। एक वह व्यक्ति जो मेरा नाम लेकर वचन दे और फिर भंग कर दे, और एक व्यक्ति वह है जो किसी स्वतन्त्र आदमी को बेच दे और उसकी क़ीमत खा जाए। और एक वह व्यक्ति जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर रखा फिर उससे काम पूरा लिया और उसे उसकी मज़दूरी न दी।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि ईश्वर तीन प्रकार के व्यक्तियों का शत्रु होगा। जिस किसी का शत्रु ईश्वर हो उसकी तबाही और बरबादी में क्या सन्देह हो सकता है। एक व्यक्ति वह है जो वचनभंग करता हो और एक वह व्यक्ति है जिसको ईश्वर की महानता का कुछ भी ध्यान न हो और जो इतना निर्लज्ज हो कि स्वतन्त्र व्यक्ति को बेचे और उसकी क़ीमत स्वयं खाए और उसकी क़ीमत खाते हुए उसे कुछ भी संकोच न हो और इस पर उसकी अन्तरात्मा इस बात को सहन कर ले कि किसी को दासता में डालकर स्वयं अपने लिए ऐश का साधन जुटाए। इस प्रकार के लोगों पर अगर उसका क्रोध न भड़केगा तो फिर किसपर भड़केगा।
तीसरा व्यक्ति वह है जो काम पूरा ले लेकिन मज़दूरी न दे। यह खुला हुआ अन्याय और अत्याचार है कि मज़दूर से काम तो पूरा लिया जाए लेकिन मज़दूरी से उसे वंचित रखा जाए। जो व्यक्ति सत्य और न्याय के विरुद्ध कोई क़दम उठाता है वह कोई साधारण गुनाह नहीं करता, बल्कि वह अपनी नीति से वास्तव में अपने ईश्वर को अपना शत्रु बनाता है, चाहे उसे इस बात का एहसास हो या न हो।
(5) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति हमें धोखा दे वह हममें से नहीं है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बाज़ार गए। वहाँ गेहूँ के एक ढेर में हाथ डाला तो उसे अन्दर से गीला पाया। दुकानदार से इसका कारण पूछा तो उसने उज़्र पेश किया कि पानी से भीग गया है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि ऐसी बात थी तो भीगे हुए गेहूँ को ऊपर क्यों न रखा (कि लोगों को धोखा न होता)? इसी अवसर पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सचेत किया कि "जो व्यक्ति हमें धोखा दे वह हममें से नहीं है।" अर्थात वह हमारे लाए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ चल रहा है। अगर वह चाहता है कि दुनिया और आख़िरत में उसकी गणना सन्मार्ग पर चलनेवाले गरोह में हो तो उसे धोखा और फ़रेबकारी के कामों से पूर्णतः बचना चाहिए।
व्यंग्य और उपहास
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कभी बन्दा एक बात कहता है और केवल लोगों को हँसाने के लिए कहता है। उसके कारण वह उस दूरी से भी बढ़कर जो आकाश और धरती के मध्य पाई जाती है, दूर जा गिरता है। और सत्य यह है कि अपने क़दमों के कारण फिसलने से कहीं गम्भीर बात बन्दे के लिए यह है कि वह अपनी ज़बान के कारण फिसल जाए।" (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : हँसने और हँसाने को अपना पेशा बनाना किसी प्रकार उचित नहीं है। और अगर इसके लिए कोई झूठ से काम लेता है फिर तो वह अपने आप पर ऐसा अत्याचार करता है जिसका परिणाम घाटे और सन्ताप के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। हास्य-विनोद और हँसी-मज़ाक़ की अधिकता से आदमी की गरिमा का ह्रास होता है। इससे उसकी गरिमा क्षतिग्रस्त होकर रह जाती है। अतएव हदीस में है—
“ज़्यादा हँसने से परहेज़ करो क्योंकि अधिक हँसना हृदय को मृतप्राय और मुख को निस्तेज कर देता है।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल ईमान)
यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि आदमी लोगों को हँसाने के उद्देश्य से अपनी आख़िरत नष्ट कर ले और उच्च स्थान से गिर जाए यहाँ तक कि नरक में जा पड़े।
आदमी चाहे कितनी ही उच्चता पर क्यों न हो, उपहास और मखौल के कारण अत्यन्त अधम होकर रहता है। इनसान को ईश्वर ने महत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण स्थान पर खड़ा किया है। फिर उसके लिए यह क्योंकर उचित हो सकता है कि वह अपने समय को व्यर्थ और ग़लत कार्यों में बिताए।
पैर फिसलने से आदमी को उतनी हानि नहीं पहुँचती जितनी जीभ की लड़खड़ाहट से पहुँच सकती है। पैर फिसलने से उसके शरीर को चोट लग सकती है लेकिन जीभ की लड़खड़ाहट से आदमी की आख़िरत तक तबाह और बरबाद हो सकती है।
(2) हज़रत बह्ज़-बिन-हकीम (रहमतुल्लाह अलैह) अपने पिता और वे बह्ज़ के दादा के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ख़राबी है उसके लिए जो बात करे तो झूठ बोले ताकि लोगों को हँसाए। ख़राबी है उसके लिए, ख़राबी है उसके लिए।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद, दारमी)
व्याख्या : चेतावनी की तीव्रता के उद्देश्य से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 'ख़राबी है उसके लिए' को दोहराया। ख़राबी के लिए मूल में ‘वैल’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। अरबवाले शब्द 'वैल' उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो अत्यन्त अप्रिय कर्म करता हो। इसका उद्देश्य खेद प्रकट करना और उसको सचेत करना होता है।
किसी को हीन समझना
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“परस्पर एक-दूसरे से ईष्या न करो, न एक-दूसरे की टोह और कुरेद में पड़ो, न आपस में द्वेष रखो, न परस्पर शत्रुता या सम्बन्ध विच्छेद करो, और न तुममें से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा करे। अल्लाह के बन्दे और आपस में भाई-भाई बनकर रहो। मुसलमान मुसलमान का भाई है। न वह उसपर अत्याचार करे, न उसे अपमानित करे, और न उसे हीन समझे। ईशभय यहाँ है।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने सीने की ओर संकेत किया। ऐसा आप ने तीन बार किया, “आदमी के लिए यही बुराई पर्याप्त है कि वह अपने मुसलमान भाई को हीन समझे। मुसलमान की प्रत्येक वस्तु दूसरे मुसलमान के लिए अवैध है, उसका रक्त, उसका धन और उसकी आबरू।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस अपने अर्थों में अत्यन्त सुस्पष्ट है। मुसलमानों के आपसी सम्बन्ध भाइयों की तरह ही होने चाहिएँ। मुसलमान एक-दूसरे की प्रतिष्ठा और गरिमा का ध्यान रखें। उनका पूरा प्रयास हो कि उनसे किसी भाई को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे।
ईशभय का असल सम्बन्ध हृदय से है। मात्र बाह्य कर्मों को नहीं बल्कि आदमी को अपने आन्तरिक दशा में भी सुधार लाने की चिन्ता करनी चाहिए जो लोगों की दृष्टि में नहीं आ पाती।
यह अत्यन्त दुखद होगा कि कोई व्यक्ति भला बनने के बजाए अपने लिए बुरा बनना पसन्द करे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह अपने भाई को हीन समझे। चाहे उसके अन्दर कोई अन्य बुराई न हो। उसके बुरा होने के लिए यही एक दोष पर्याप्त है कि वह अपने भाई को हेय दृष्टि से देखता है।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“कितने ही बिखरे केशोंवाले, धूल-धूसरित और द्वारों पर से धकेले गए लोग ऐसे हैं कि अगर वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए किसी बात पर सौगन्ध खा लें तो ईश्वर उसे पूरा कर दे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मतलब यह है कि दुनिया के ग़रीबों और फटेहाल लोगों को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनमें अल्लाह के प्रिय बन्दे भी हो सकते हैं जिनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखकर लोग उन्हें धक्के देते हैं, हालाँकि उनके ईश्वरप्रिय होने का हाल यह है कि अगर वे किसी बात पर क़सम खा बैठें तो अल्लाह अनिवार्यतः उनकी क़सम को पूरा कर देगा। उनको कदापि निराश और लज्जित न होने देगा।
(3) हज़रत इयाज़-बिन-हिमार मुजाशिई (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने मेरी ओर प्रकाशना की है कि विनयशीलता अपनाओ यहाँ तक कि कोई व्यक्ति किसी के मुक़ाबले में गर्व न करे और न कोई किसी पर अत्याचार और ज़्यादती करे।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मुझपर इस बात की प्रकाशना की है कि लोग विनम्रता और विनयशीलता की नीति अपनाएँ और अहंकार और घमंड से अपने आप को दूर रखें। कोई किसी के मुक़ाबले में न तो अभिमान करे और न किसी पर अत्यचार करे। बन्दे के लिए जो वस्त्र शोभा देता है वह विनम्रता का वस्त्र है। दूसरे परिधान, यथा अहंकार, गर्व, घमंड आदि धारण कर बन्दा अपना स्वाभाविक सौन्दर्य खो देता है।
मानहानि
(1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो मुसलमान व्यक्ति किसी मुसलमान व्यक्ति की उस अवसर पर सहायता न करे जहाँ उसका अनादर किया जाता हो और उसकी आबरू को हानि पहुँचाई जाती हो तो अल्लाह उसकी उस अवसर पर सहायता नहीं करता जहाँ वह उसकी सहायता का इच्छुक होता है, और जो मुसलमान व्यक्ति किसी मुसलमान व्यक्ति की उस अवसर पर सहायता करे जहाँ उसका अनादर किया जाता हो और जहाँ उसकी आबरू को हानि पहुँचाई जाती हो तो सर्वोच्च अल्लाह उसकी उस अवसर पर सहायता करेगा जहाँ वह चाहता है कि उसे उसकी सहायता प्राप्त हो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात जैसा व्यवहार किसी का अपने भाई के प्रति होता है उसके साथ ईश्वर का व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। कोई अपने भाई की ऐसे अवसर पर प्रतिरक्षा करता है जहाँ उसका अनादर और उसकी मर्यादा का हनन हो रहा हो तो ईश्वर भी (दुनिया और आख़िरत) में ऐसे अवसर पर उसकी सहायता करेगा जहाँ उसे सहायता और अनुकम्पा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। लेकिन अगर वह अपने मुसलमान भाई की मान-मर्यादा की कोई चिन्ता नहीं करता। भाई की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाए जा रहे हों लेकिन वह अपने भाई की सहायता के लिए खड़ा नहीं होता और उसकी ओर से प्रतिरक्षा का कोई प्रयास नहीं करता, तो फिर उसको भी ईश्वर से इसकी आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह कभी उसकी ऐसे मौक़े पर सहायता करेगा। जो व्यक्ति अपने भाई के काम नहीं आता वह वास्तव में इसकी पात्रता खो देता है कि ईश्वर कठिनाई में उसकी सहायता को पहुँचे।
(2) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“जो मुसलमान अपने भाई के सम्मान की रक्षा हेतु प्रतिरक्षा करता है तो अनिवार्यतः अल्लाह पर यह हक़ हो जाता है कि क़ियामत के दिन वह नरक की अग्नि से उसकी रक्षा करे और नरक की अग्नि को उससे दूर रखे।" फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ुरआन की यह आयत पढ़ी—
"ईमानवालों की सहायता तो हमपर एक हक़ है" (30:47)। (हदीस : शरहस्सुन्नाह)
व्याख्या : नरक की अग्नि में जलना यातना के अतिरिक्त बड़े अपमान का विषय भी है। जो व्यक्ति दुनिया में अपने भाई को अपमानित होने से बचाता और उसके लिए पूरा प्रयास करता है, ईश्वर भी ऐसे नेक और भलेमानस व्यक्ति को आख़िरत के अपमान और यातना से सुरक्षित रखेगा। लोगों को सम्मान प्रदान करनेवाला कभी अपमानित नहीं हो सकता। और यह भी एक वास्तविकता है कि जो व्यक्ति दूसरों की मानहानि पर उतर आता है, वह अन्ततः स्वयं अपमानित होकर रहता है।
(3) हज़रत सईद-बिन-ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सबसे बढ़कर ब्याज यह है कि मुसलमान को नाहक़ बेआबरू करने के लिए ज़बान चलाई जाए।" (हदीस : अबू-दाऊद, अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : क्रय-विक्रय और ऋण के सिलसिले में उचित और मूलधन से अधिक वसूल करने को ब्याज कहा जाता है। इस्लाम की दृष्टि में ब्याज के द्वारा अपने धन में बढ़ोत्तरी करना बिल्कुल अवैध, अमानुषिक और ईश्वरीय प्रकोप को भड़कानेवाला अपराध और पाप है। किसी इनसान को यह अधिकार नहीं कि वह अपने ऋणी से अपने दिए हुए धन से अधिक की माँग करे। ठीक इसी प्रकार किसी को यह अधिकार नहीं पहुँचता कि वह अनाधिकार किसी मुसलमान की मानहानि पर उतारू हो और उसके लिए ज़बानदराज़ी करे। वास्तविकता की दृष्टि में यह ज़बानदराज़ी निकृष्टतम ब्याज है। साधारण ब्याज में आदमी को आर्थिक हानि पहुँचती है जबकि यह सूद ऐसा है जिसमें आदमी की प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा को आघात पहुँचता है। आर्थिक हानि के मुक़ाबले में मान-मर्यादा की हानि ज़्यादा सख़्त और अत्यन्त दुखदायी होती है। इसलिए अगर किसी की अनुचित मानहानि के लिए की जानेवाली ज़बानदराज़ी को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने निकृष्टतम सूद ठहराया है तो यह वास्तविकता का सर्वाधिक सत्यानुकूल चित्रण है।
दुख और हानि पहुँचाना
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ (के उत्पीड़न) से समस्त मुस्लिम सुरक्षित रहें। और मुहाजिर वह है जो उन बातों को छोड़ दे जिनसे ईश्वर ने मना किया है।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : तिर्मिज़ी और नसई में ये अतिरिक्त शब्द भी मिलते हैं—
“मोमिन वह है जिसको लोग अपनी जान और माल के बारे में अमानतदार समझें।”
अपने अर्थ के लिहाज़ से यह हदीस अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक गुण भी इस हदीस में पाए जाते हैं। शब्द मुस्लिम की धातु (Root) वही है जो सिल्म शब्द की धातु है। इसलिए मुसलमान को सर्वथा शान्ति और सलामती की प्रतिमूर्ति होना चाहिए, न यह कि उससे यह भय बना रहे कि कहीं वह अपने भाइयों की सुख-शान्ति पर डाका डालने लग जाए।
मुस्लिम सही अर्थों में वही व्यक्ति है जिससे किसी को किसी भी प्रकार की हानि और दुख की आशंका न हो। इस हदीस में ज़बान और हाथ का उल्लेख इसलिए किया गया है कि उत्पीड़न में साधारणतः जीभ और हाथ ही से काम लिया जाता है वरन् उत्पीड़न चाहे किसी भी रूप में दिया जाए वह अवैध ही होगा।
मोमिन शब्द और अमन शब्द की धातु भी एक ही है। इसलिए मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि उसपर विश्वास और भरोसा किया जा सके।
इस्लाम की शिक्षाओं के अध्ययन से मालूम होता है कि ईश्वर अपने बन्दे से इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि वह अपनी बन्दगी, उपासना, समर्पण और आज्ञाकारिता को ईश्वर के लिए आरक्षित कर ले। वह ईश्वर ही की स्तुति करे और उसकी महानता और पवित्रता का वर्णन करे। उसी के आगे नतमस्तक हो। उसके दिल में अपने प्रभु के लिए अत्यन्त नम्रता, प्रेम और आसक्ति की भावना पाई जाती हो। नमाज़, रोज़ा और हज आदि इबादत ईश्वर ही के लिए अनिवार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समस्त धार्मादेशों में जो प्रयोजन रखा गया है। वह मानव जाति ही की आवश्यकताएँ हैं। ईश्वर अपने बन्दों पर अत्यन्त कृपाशील है। वह अपने बन्दों से गहरा सम्बन्ध रखता है। यही कारण है कि धर्म का बड़ा भाग लोगों की भलाई और कल्याण से सम्बन्धित है। यद्यपि ईशपरायणता और ईश-आकांक्षा की भावना हर जगह अपेक्षित है। इस्लाम में लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना ठीक दीन और ईमान है। किसी मुस्लिम के लिए यह सही न होगा कि वह अपने भाइयों से कोई दिलचस्पी न रखे कि न वह उनके दुख-दर्द को अपना दुख-दर्द समझे और न उनके सुख और प्रसन्नता से उसे कोई सरोकार हो। यह ईश-परायणता की भावना के भी प्रतिकूल है। इसलिए कि जिस ईश्वर की महानता और बड़ाई को हम स्वीकार करते हैं, जब स्वयं उसे अपने बन्दों से प्रेम है तो हमारे लिए यह कैसे जायज़ हो सकता है कि हम ईश्वर के बन्दों के रंज और राहत का कुछ ध्यान न रखें।
ईश्वर की प्रसन्नता और उसके धर्म के लिए मातृभूमि और धन-सम्पत्ति के त्याग का महत्व अपनी जगह है लेकिन अगर हमने उन बुराइयों को नहीं छोड़ा और हम उन चीज़ों के त्याग के लिए तैयार न हुए जो अल्लाह को प्रिय नहीं हैं तो वास्तव में हम हिजरत की मूल भावना और उसकी आत्मा से अपरिचित ही रहे।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तुम जानते हो कि दरिद्र कौन है?” लोगों ने कहा कि हममें दरिद्र वह है जिसके पास न दिरहम हो और न सम्पत्ति और साधन। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "मेरी उम्मत में असली दरिद्र वह है जो क़ियामत के दिन इस अवस्था में उपस्थित हो कि उसके पास नमाज़-रोज़ा और ज़कात सब हो मगर वह किसी को गाली देकर आया हो, किसी पर मिथ्या दोषारोपण कर, किसी का माल हड़पकर, किसी का रक्त बहाकर और किसी को पीटकर आया हो। फिर उसकी एक-एक नेकी मज़लूमों में बाँट दी जाएगी इससे पूर्व कि जो बदला उसे चुकाना है वह चुकाया जाए। अगर उसकी नेकियाँ समाप्त हो जाएँगी तो मज़लूमों के गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएँगे और फिर वह नरकाग्नि में फेंक दिया जाएगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि असली दरिद्र वह नहीं जिसके पास यहाँ धन-सम्पत्ति न हो। बल्कि असली दरिद्र वह है जिसे आख़िरत में दरिद्र घोषित किया जाए। उसने अगर दुनिया में नेकियाँ की भी हों तो वह उसके अत्याचारों के कारण उससे छीन कर उन मज़लूमों में बाँट दी जाएँगी जिनपर उसने अत्याचार किए थे और फिर भी अगर हिसाब चुकता न हो तो मज़लूमों के गुनाह और उनकी ख़ताएँ उसके हिसाब में डाल दी जाएँगी और उसके पास कुछ भी न होगा जो उसे नरकाग्नि से बचा सके।
धिक्कार एवं भर्त्सना
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास से गुज़रे। उस समय हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने किसी ग़ुलाम पर लानत कर रहे थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनकी ओर रुख़ करते हुए कहा—
“लानत करनेवाले और सिद्दीक़ीन! काबा के प्रभु की सौगन्ध, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।" यह सुनकर हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने (अपनी कोताही के प्रायश्चितस्वरूप) अपने कुछ ग़ुलामों को स्वतन्त्र कर दिया और फिर (क्षमायाचना के लिए) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूँगा।” (हदीस : अल-बैहक़ी फ़ी शोअ'बिल-ईमान)
व्याख्या : “लानत करनेवाले और सिद्दीक़ीन!" अर्थात यह क्या देख रहा हूँ? जो व्यक्ति सत्यवान हो क्या उसकी ज़बान पर धिक्कारपूर्ण शब्द कभी आ सकते हैं!
यह कदापि नहीं हो सकता कि दोनों बातें एकत्र हों। कोई सिद्दीक़ (सत्यवान) भी हो और धिक्कारनेवाला भी हो। मतलब यह है कि ऐ अबू-बक्र! तुम तो सिद्दीक़ हो, फिर यह क्या कर रहे हो कि अपने दास को धिक्कार रहे हो! सिद्दीक़ को तो ऐसा नहीं होना चाहिए!
यह हदीस बताती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दृष्टि में हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को सिद्दीक़ियत का स्थान प्राप्त था जो नुबूवत के बाद सर्वाधिक उच्च और श्रेष्ठ स्थान है।
सिद्दीक़े अकबर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि भविष्य में मुझे किसी को धिक्कारते हुए नहीं देखेंगे।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"सिद्दीक़ को शोभा नहीं देता कि वह बहुत अधिक धिक्कारने वाला हो।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मूल में “लअ्आन” शब्द आया है जिसका अर्थ है बहुत अधिक लानत करनेवाला, जिसकी आदत ही लानत करने की हो। सिद्दीक़ भी अतिशयोक्ति का एक रूप है। इसका अर्थ होता है— बहुत ही सच्चा। हदीस का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सत्य के गुण से सुसज्जित हो और जिसको नुबूवत से सान्निध्य प्राप्त हो चुका हो उसके मर्यादानुकूल यह बात कदापि नहीं हो सकती कि वह दूसरों पर लानत करता फिरे। लानत करने का अर्थ यह है कि हम किसी को ईश्वरीय अनुकम्पा एवं सामीप्य से वंचित और दूर क़रार दे रहे हैं जबकि अल्लाह के रसूलों और उनके सच्चे अनुयायियों की गतिविधियों का प्रयोजन कुछ और ही होता है। वे तो ईश्वर के बन्दों को ईश्वर की अनुकम्पा से निकट करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत होते हैं।
(3) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का वर्णन है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
"बहुत ज़्यादा लानत करनेवाले क़ियामत के दिन न गवाह बन सकेंगे और न सिफ़ारिश कर सकेंगे।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ऐसे लोग जिनका स्वभाव ही धिक्कारना है उन्हें क़ियामत के दिन यह सम्मान प्राप्त न होगा कि वे किसी की सिफ़ारिश कर सकें या उन्हें उस दिन गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हालाँकि मुस्लिम समुदाय को अल्लाह ने “शु-हदा-अ अलन्नास” (सम्पूर्ण मानवजाति पर गवाह) की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया है। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव ही धिक्कारना है वे इस श्रेय से उस दिन वंचित होंगे।
(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! बहुदेववादियों को शापित कीजिए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि मैं तो मात्र रहमत (सर्वथा दयालुता) बनाकर भेजा गया हूँ।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मेरे अवतरित होने का मूल प्रयोजन तो यह है कि मैं ईश्वर के द्वारा अवतरित मार्गदर्शन और नैतिक शक्ति के द्वारा लोगों को ईश्वरीय अनुकम्पा का भागीदार बनाऊँ। फिर मैं किसी पर लानत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अवज्ञाकारियों के लिए भी यही प्रार्थना करूँगा कि वे सत्य मार्ग पर चलने लगें।
क़ुरआन में है—
“हमने तुम्हें सारे संसार के लिए बस सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा है।" (21:107)
ईमानवालों के लिए तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अस्तित्व ईश्वरीय अनुग्रह का निमित्त है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अस्तित्व धर्म के शत्रुओं के लिए भी सर्वथा दयालुता ही है। विगतकाल की अवज्ञाकारी और विद्रोही क़ौमों को ईश्वर ने पूर्णतः विनष्ट कर दिया था लेकिन यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वुजूद की बरकत है कि सत्यद्रोहियों का समूल नाश नहीं हुआ। धरती में उन्हें शेष रखा गया, उनको सत्यधर्म की ओर आमन्त्रित करने हेतु नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने पीछे मुस्लिम समुदाय का एक महान गरोह छोड़ा है। यह मानवजाति पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सबसे बड़ा उपकार है।
(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जब कोई व्यक्ति यह कहे कि लोग हलाक हुए तो वह स्वयं सबसे बढ़कर हलाक होनेवाला है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात जो व्यक्ति यह कहता है कि लोग हलाक हुए और उसके इस कहने के पीछे कोई सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव नहीं पाया जाता और न उसकी यह कामना ही होती है कि लोग तबाही और हलाकत के रास्ते के बजाए कल्याण और भलाई के रास्ते पर चलें, बल्कि यह बात वह दोषान्वेषण की अपनी दुर्भावना और लोगों को हीन बनाने के उद्देश्य से कहता है और इससे उसका वास्तविक प्रयोजन अपने अहं भाव की तृप्तिमात्र होता है तो इस अवस्था में वह स्वयं अपने लिए सबसे बढ़कर हलाकत की सामग्री जुटा रहा होता है, यद्यपि उसे इसका आभास नहीं होता।
अरबी मूल में अगर “अह-लकुहुम" के स्थान पर "अह-ल-कहुम" पढ़ा जाए, जैसा कि कुछ रिवायतों में उद्धृत हुआ है, तो इस सूरत में अनुवाद यह होगा कि इस प्रकार कहनेवाला उन्हें (अर्थात लोगों को) हलाक कर देता है। मतलब यह है कि वह यह कहकर कि “लोग हलाक और बरबाद हो गए" लोगों में क्षोभ और निराशा का वातावरण बनाता है और उन्हें बेशौक़ और हतोत्साहित करता है जिसका परिणाम यह होगा कि लोग अपने मार्गदर्शन और कल्याण से बिल्कुल निराश होकर गुनाहों और बुराइयों में और अधिक लिप्त हो जाएँगे और आख़िरत की चिन्ता से पूर्णतः विलग हो जाएँगे। अतएव जो व्यक्ति भी लोगों के बारे में ऐसी निराशाजनक और निरुत्साहित करनेवाली बातें कहता है वह लोगों का मित्र और शुभचिन्तक नहीं हो सकता बल्कि वह उनको हलाकत में डालने का सबसे बड़ा कारण स्वयं बन रहा होता है।
(6) हज़रत साबित-बिन-ज़ह्हाक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी मोमिन पर लानत करना ऐसा ही है जैसे उसकी हत्या कर देना।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात किसी मोमिन व्यक्ति पर लानत करना एक प्रकार से उसे मौत के घाट उतारना है। किसी पर लानत करने का अर्थ यह होता है कि लानत करनेवाला उसे ईश्वर की अनुकम्पा और सामीप्य से दूर और प्रतापवान ईश्वर की बारगाह से उसे वंचित ठहराता है। किसी मोमिन के लिए इससे बढ़कर दूसरी मृत्यु क्या हो सकती है कि वह ईश्वर की दृष्टि में पतित हो जाए और उसकी अनुकम्पा के स्थान पर उसके प्रकोप का भागी बने। विधर्मी तो बिना मारे ही मृत होते हैं। वे जीवन के वास्तविक आशय से अनभिज्ञ होकर जीवनयापन करते हैं। इसके विपरीत मोमिन को वास्तविक जीवन प्राप्त होता है। वह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। ईश्वर से उसका जीवन्त सम्बन्ध होता है। वह उसके सामीप्य का अधिकारी होता है। अब अगर कोई उसपर लानत करता है तो इसका अर्थ इसके सिवा और क्या होगा कि वह उसे उस जीवन से वंचित कर रहा है जो ईश्वर सम्बन्ध और उसकी विशिष्ट अनुकम्पा के निमित्त संसार में केवल मोमिन को प्राप्त होती है।
(7) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमें सम्बोधित किया, उसमें स्त्रियों से आपने कहा—
“ऐ स्त्रियो, तुम सद्क़ा करो, क्योंकि क़ियामत के दिन नरकवालों में तुम्हारी बहुतायत होगी।" इसपर एक स्त्री, जो ऊँचे दर्जे की न थी (आम औरतों में से थी), खड़ी हो गई और उसने निवेदन किया कि नरकवालों में हम औरतों की बहुतायत किस कारण होगी? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "इसलिए कि स्त्रियाँ अधिक लानत करती रहती हैं और अपने पतियों के प्रति अकृतज्ञता प्रदर्शित करती हैं।" (हदीस : मुस्नद अहमद)
व्याख्या : अर्थात स्त्रियों में यह कमज़ोरी साधारणतः देखने में आती है कि दूसरों पर नुक्ताचीनी और उनमें दोष निकालना उनका दिल पसन्द काम होता है। फिर वे साधारणतः अपने पतियों के प्रति अकृतज्ञता भी प्रकट करती रहती हैं। तनिक भी उनके स्वभाव के विरुद्ध कोई बात हुई नहीं कि वे पति के समस्त उपकारों को पूर्णतः विस्मृत कर बैठती हैं कि मेरा दुर्भाग्य ही है कि तुम्हारे हाथ पड़ी।
दुष्भाषिता
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुसलमान के साथ दुर्वचनों का प्रयोग, अवज्ञा और उससे युद्ध करना अधर्म है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात किसी मुसलमान के साथ दुर्वचनों का प्रयोग करना और उसे गाली देना अवज्ञाकारियों का काम है। यह किसी मोमिन को शोभा नहीं देता कि वह अपने भाई को दुर्वचनों की भेंट दे। मुसलमान से लड़ना और अन्यायपूर्वक उसका रक्त बहाना भी अत्यन्त गम्भीर अपराध है। यह काम मोमिन का नहीं, विधर्मियों का है कि वह किसी मुसलमान की हत्या पर उतारू हो जाए।
(2) हज़रत अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“जो व्यक्ति किसी को काफ़िर कहकर पुकारे या उसे ईश्वर का शत्रु कहे और वह व्यक्ति वास्तव में ऐसा न हो तो उसका कहा हुआ स्वयं उसी पर लौट आता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि जो व्यक्ति किसी को काफ़िर कहकर पुकारता है या उसे ईश्वर के शत्रु के नाम से याद करता है वह अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहा है। इसलिए कि अगर वह व्यक्ति वास्तव में काफ़िर और ईश्वर का शत्रु नहीं है तो उसके ऐसे नाम धरनेवाला स्वयं ईश्वर की दृष्टि में काफ़िर और सत्य का बैरी होगा।
(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अपने माता-पिता को गाली देना कबीरा (बड़े) गुनाहों में से है।” लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को भी गाली दे सकता है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा— "हाँ, एक व्यक्ति दूसरे के बाप को गाली देता है, जवाब में वह उसके बाप को गाली देता है और ये उसकी माँ को गाली देता है तो वह जवाब में उसकी माँ को गाली देता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात जिसने गाली देने में पहल की उसने दूसरे के लिए इसका अवसर प्रदान कर दिया कि वह उसके माता-पिता को गालियाँ दे। मानो दूसरे ने नहीं बल्कि उसने स्वयं अपने माता-पिता को गाली दी। वास्तव में जो व्यक्ति भी किसी काम का कारण बनता है वही उसका उत्तरदायी भी होता है। जिस कार्य का परिणाम स्वयं अपने लिए बुरा हो, उससे बचना अनिवार्य है।
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन कोटि की दृष्टि से निकृष्टतम व्यक्ति वह होगा जिसे लोग उसकी बुराई के कारण त्याग दें।" एक हदीस में है कि "जिसके अश्लील वचनों के भय से लोग उससे दूर-दूर रहें।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यह एक लम्बी हदीस का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कौन पसन्द कर सकता है कि क़ियामत के दिन जबकि लोगों के भाग्य का अन्तिम निर्णय किया जाएगा उस दिन सृष्टिजन में वह सर्वाधिक निकृष्टतम व्यक्ति घोषित हो। इस हदीस में उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है जिनकी बुराई से लोग पनाह माँगते हों और उनसे विलग हो जाते हों। इसी तरह ऐसे लोगों के लिए भी इसमें चेतावनी है जिनकी अश्लील बातों और दुर्वचनों से तंग आकर लोग उनसे दूर ही रहना पसन्द करते हों।
(5) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क़ियामत के दिन मोमिन की तुला में रखी जानेवाली सर्वाधिक वज़नदार चीज़ सुशीलता होगी। और अल्लाह को उस व्यक्ति से घृणा और शत्रुता है जो निर्लज्जता की बातें मुख से निकालता और अनर्गल बोलता हो।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
व्याख्या : मानव स्वभाव के समस्त अपेक्षित गुणों में मौलिक और आधारभूत गुण सुशीलता और नैतिक सौन्दर्य है। अन्य सभी गुण वास्तव में इसी से सम्बन्ध रखते हैं। सुशीलता की वैश्विकता और उसकी विस्तीर्णता को समझने की आवश्यकता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मिसाल के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नैतिक सौन्दर्य से वंचित व्यक्ति की क्या दशा होती है। और ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य और अभाव संवेदनशील व्यक्तियों को कितना कंपित कर देनेवाला हो सकता है।
नैतिक सौन्दर्य से वंचित व्यक्ति मात्र दुर्वचनों और अनर्गल शब्दों का उच्चारण ही नहीं करता वरन् उसकी करतूतों की सूची बहुत लम्बी हो सकती है। उसके घिनावने कृत्य केवल इन दो बुराइयों तक ही सीमित नहीं रहते जिनका उल्लेख इस हदीस में किया गया है। यहाँ, जैसा कि कहा गया, उदाहरण मात्र के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसकी दो ऐसी बुराइयों का उल्लेख किया है जिन्हें बुराई समझने में किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं हो सकती।
(6) हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“लज्जा और मितभाषिता और सुसंकोच ईमान की दो शाखाएँ हैं और दुष्भाषिता और अनर्गल भाषण और वाक्चातुर्य कपटाचार की दो शाख़ाएँ हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मोमिन में लज्जा भी होती है और ईश्वर का भय भी होता है। उसे अपने एक-एक वाक्य के बारे में यह संशय लगा रहता है कि कहीं ईश्वर के यहाँ इसपर उसकी पकड़ न हो जाए। नाममात्र के लिए भी उसके वार्तालाप में कृत्रिमता नहीं पाई जाती। उसकी बात-चीत में सहजता और स्वाभाविकता पाई जाती है। उसकी बातों में तेज़ी और तर्रारी नहीं होती। वह जो कुछ कहता है दायित्व के साथ कहता है। लेकिन कपटाचारी का मामला इससे नितान्त भिन्न होता है। न उसमें लज्जा होती है, न कोई संकोच। अगर उसे अवसर मिल जाए तो अत्यन्त बेबाकी के साथ बढ़-चढ़कर निस्संकोच बोलते चले जाने में उसे कोई हिचक न होगी।
मुलाक़ात न करना
(1) हज़रत अबू-अय्यूब अनसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"किसी व्यक्ति के लिए जाइज़ नहीं कि वह तीन दिन से अधिक अपने भाई से मिलना-जुलना छोड़े रखे, और अवस्था यह हो कि वे कभी एक-दूसरे के सामने आ भी जाएँ तो एक अपना मुँह दूसरी ओर फेर ले और दूसरा भी अपना मुँह किसी और तरफ़ कर ले। और उन दोनों में बेहतर व्यक्ति वह है जो सलाम में पहल करे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : मानव स्वभाव में स्वाभिमान, क्रोध और पक्षधरता का जो तत्व पाया जाता है वह हर हाल में अपना प्रभाव दिखाता है। इसी लिए तीन दिन का अवसर दिया गया है ताकि इनसान अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण पा सके या कम से कम भाई से नाराज़ी और उसके प्रति क्रोध की भावना हल्की पड़ जाए और सुलह-सफ़ाई की सूरत पैदा हो सके। अलबत्ता अगर मुलाक़ात में किसी बड़े उपद्रव और ख़राबी की आशंका हो या यह किनाराकशी किसी महान धार्मिक निहितार्थ हेतु हो तो विद्वानों की दृष्टि में मुलाक़ात न करने की अवधि लम्बी भी हो सकती है और यह धर्म विरुद्ध न होगा।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं कि दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। एक दूसरी हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“सलाम में पहल करनेवाला अहंकार और घमंड से मुक्त होता है।"
जिसने सलाम में पहल की और इस प्रकार नाराज़ी दूर करने के लिए सुलह और सफ़ाई की कोशिश की उसने अपने इस कर्म से विशालहृदयता का परिचय दिया। जो हृदय विशाल हो उसमें अहंकार और घमंड के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"किसी मुस्लिम के लिए यह बात वैध नहीं कि वह अपने भाई को तीन दिन से अधिक छोड़े रखे। अतएव जिस किसी ने तीन दिन से अधिक (अपने भाई को) छोड़े रखा और इस बीच वह मर गया तो वह नरक में प्रविष्ट हुआ।" (हदीस : मुस्नद अहमद, अबू-दाऊद)
व्याख्या : सम्बन्ध विच्छेद की नीति अपनाना साधारण अर्थों में केवल अनैतिकता नहीं है बल्कि यह इस्लामी सामूहिकता की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल भी है। इसलिए इस अपराध को अत्यन्त गम्भीर घोषित किया गया है। अपने भाई से सम्बन्ध विच्छेद करके आदमी समाज में एक ऐसी ग़लत मिसाल क़ायम करता है जो सामाजिकता की जड़ को काटनेवाली होती है।
हालाँकि हमें अपने जीवन में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिएँ जिनसे सामूहिकता सुदृढ़ हो सके।
फिर सम्बन्ध विच्छेद के कारण आदमी अपने भाई के वे अधिकार प्रदान करने में असमर्थ रहता है जिन्हें प्रदान करना उसका दायित्व होता है और इस प्रकार स्वयं उसे भी अपने भाई से कोई लाभ नहीं पहुँच सकता।
जगत् की व्यवस्था जिस क़ानून के तहत चल रही है उसमें किसी प्रकार की अनुदारता और तंगी नहीं पाई जाती। अगर ईश्वर की अपार दयालुता न हो तो हमारा अस्तित्व ही शेष नहीं रह सकता। अब यह बहुत बड़ा अत्याचार होगा कि जिस नियम पर हमारा अस्तित्व निर्भर करता है हम उसी नियम का विरोध करने लग जाएँ। हम उसी शाखा को काटने लगें जिसपर हम स्वयं बैठे हुए हों। हम अपने ईश्वर से जिस क्षमा और दानशीलता की आशा रखते हों उसके लिए अपेक्षित यह है कि हम लोगों की उन आशाओं को आहत न होने दें जो आशाएँ उन्हें स्वाभाविक रूप से हमसे होती हैं।
झगड़ालू मानसिकता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह की दृष्टि में सर्वाधिक घृणित और अप्रिय व्यक्ति वह है जो हठी प्रकार का झगड़ालू हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : ऐसा व्यक्ति किसी भी समाज और समुदाय के लिए एक मुसीबत होता है जिसको बस झगड़ा करने ही में आनन्द आता हो और जो हर समय लोगों से झगड़ने के लिए तैयार रहता हो। झगड़ालू मानसिकता रखनेवाला व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ सकता। वह हर समय अपना मानसिक सन्तुलन खोए ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती। ऐसा संकीर्णहृदय व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में सर्वाधिक अप्रिय होता है।
(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तेरे लिए यही गुनाह पर्याप्त है कि तू हमेशा झगड़ता ही रहे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतनी-सी बात पर्याप्त है कि वह झगड़ालू मानसिकता का हो और लोगों से हमेशा लड़ता-झगड़ता रहता हो। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी और गुनाह में लिप्त हो या न हो, ईश्वर की दृष्टि में उसके गुनाहगार होने के लिए यही एक बुराई बहुत है कि वह झगड़ालू क़िस्म का आदमी है।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह तुम्हारे लिए तीन बातों को पसन्द करता और तीन को नापसन्द करता है।" एक हदीस में ये शब्द हैं कि वह तीन बातों के कारण तुम पर क्रुद्ध होता है। उसने जो चीज़ें तुम्हारे लिए पसन्द की हैं वे ये हैं कि तुम उसी की बन्दगी अपनाओ और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक न ठहराओ, और यह कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को दृढ़तापूर्वक थाम लो और फूट में न पड़ो। और यह कि उसके हितैषी हो जिसको ईश्वर ने तुमपर शासक बनाया हो। और उसने तुम्हारे लिए जो वस्तुएँ नापसन्द की हैं वे ये हैं— 'क़ीलो-क़ाल,' अत्यधिक सवाल और बरबादि-ए-माल।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इस्लामी शासन-व्यवस्था की यह प्रमुख विशिष्टता है कि उसमें शासक और शासित के पारस्परिक सम्बन्ध को मात्र बाह्य अनुशासनों ही की हद तक अपेक्षित नहीं समझा गया है बल्कि यह अनिवार्य ठहराया गया है कि उनके सम्बन्धों का वास्तविक आधार प्रेम और शुभाकांक्षा हो क्योंकि इसके बिना मधुर परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। शासक को अपने शासित वर्ग का शुभचिन्तक होना चाहिए और शासित वर्ग को भी चाहिए कि वह अपने शासक का हितैषी हो। लेकिन शासक की पोज़ीशन चूँकि अत्यन्त नाज़ुक होती है इसलिए वह इसका ज़्यादा हक़दार होता है कि उसके साथ सहयोग किया जाए और उसके साथ मामला सदैव ख़ैरख़ाही का हो।
इस हदीस में जिन तीन अप्रिय बातों का उल्लेख किया गया है उनमें पहली चीज़ का सम्बन्ध आदमी के विचार और उसकी मानसिक अवस्था से है। दूसरी चीज़ का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से आदमी की नैतिकता और उसके चरित्र से है। और तीसरी चीज़ इस बात से सम्बन्धित है कि आदमी अपना व्यावहारिक जीवन दायित्वपूर्ण ढंग से व्यतीत करता है या नहीं। ये तीन बातें अनुप्रास (क़ाफ़िए) के रूप में बयान हुई हैं, इसलिए उनको आसानी के साथ याद रखा जा सकता है।
पहली चीज़ जो अल्लाह को नापसन्द है वह है क़ीलो-काल, अर्थात व्यर्थ की बातें और अनर्गल तर्क-वितर्क किसी बात में अनुचित खोज-कुरेद, अनावश्यक बहस और हुज्जतबाज़ी अत्यन्त नापसन्दीदा चीज़ है। यह विकृत मन का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो क़ीलो-काल का रसिया होता है उसे बस इसी में दिलचस्पी होती है। दीर्घ वार्तालाप, बाल की खाल निकालना और हर बात में कीड़े निकालना ही उसकी प्रिय व्यस्तता हो जाती है। उसकी शक्ति और उर्जा का बड़ा भाग क़ीलो-क़ाल की भेंट होकर रह जाता है। उसके यहाँ गहन सोच-विचार और अज्ञापालन की भावना और प्रतिभा आहत होकर रह जाती है। उसमें एक प्रकार का घमंड भी पैदा हो जाता है। वह हर बात में दोष निकालने ही को अपनी विजय समझता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी हानिकर होता है। कितने ही लोग उसकी बातों के झांसे में आ जाते हैं और वही असन्तुलन उनके अन्दर भी प्रवेश कर जाता है। वह उनकी अभिरुचि और स्वभाव को भी बिगाड़कर रख देता है। एक बड़ी हानि इससे यह होती है कि आदमी धर्म के वास्तविक आनन्द से वंचित होकर रह जाता है। धर्म निरर्थक तर्क-वितर्क और व्यर्थ शास्त्रार्थों में नहीं पाया जाता। धर्म तो हृदय की सर्वोत्तम भावनाओं और निःस्वार्थ आज्ञापालन का नाम है। अनुचित तर्क-वितर्क दिल को तबाह करके छोड़ता है। मुस्लिम समुदाय के सर्वोत्तम लोग वे थे जो ईश्वर और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रत्येक आदेश का पालन करते और अपनी पूरी जान से उसे अपनाते थे। उन्होंने सत्य को काग़ज़ के पन्नों से अधिक ज़िन्दगी की किताब में सुरक्षित रखा। यही कारण है कि न तो वे सत्य के ज्ञान से वंचित रहे और न उनका जीवन उससे अस्पर्शित रहा। सत्य की रक्षा उनकी निगाहों और उनकी अभिरुचि ने ही नहीं की बल्कि उनका सम्पूर्ण जीवन ही सत्य की रक्षा में व्यतीत हुआ।
सहाबा का यह हाल था कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता तो उनके मुख पर यही बात आती कि "अल्लाह और रसूल ज़्यादा जानते हैं।" बाद के युग में व्यर्थ तर्क-वितर्क बढ़ा लेकिन इसके साथ एक गरोह ऐसा मौजूद था जिसने धर्म की मूल आत्मा को जीवित रखने का प्रयास किया। लेकिन हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें समाज जिस परिस्थिति से दोचार है वह आपसे छिपी नहीं।
दूसरी चीज़ जो ईश्वर को नापसन्द है, वह है अत्यधिक सवाल। सवाल की अधिकता तंगी का सबब बनती है। सवाल से अधिक ध्यान अपने कर्म और अपने सुधार पर देना चाहिए। स्वयं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अनुचित प्रश्नों से रोका था और कहा था कि जो कहा जाए उसपर अमल करो। सवाल करके धर्म में तंगी न पैदा करो। सवाल करने के बाद यदि निश्चित उत्तर दे दिया गया तो फिर उसमें किसी दूसरे तरीक़े को अपनाने की गुंजाइश बाक़ी न रहेगी। और अगर पैग़म्बर ने किसी मामले में निश्चित बात नहीं कही है तो उसमें लोग अपनी समझ के मुताबिक़ काम करेंगे। उसमें मतभेद भी होगा किन्तु इस मतभेद से धर्म में कुशादगी और व्यापकता आएगी। यह मतभेद अलगाव और उपद्रव का कारण नहीं बनेगा।
धार्मिक मामलों में अनुचित और बहुतायत से सवाल करने को जिस प्रकार अप्रिय कहा है उसी प्रकार उस सवाल के आधिक्य को भी पसन्द नहीं किया गया जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के उद्देश्य से लोगों से माँगता और उनके सामने अपना दामन फैलाता है। आदमी को यथासम्भव माँगने से बचना चाहिए और अगर विवश होकर याचना करनी ही पड़े तो इस सम्बन्ध में अपने सदाचारी और ईमानवाले भाइयों ही से माँगे। लेकिन जहाँ तक सम्भव हो लोगों का एहसान न ले। माँगने को पेशा बनाना तो किसी मृत्यु से कम नहीं है। जो व्यक्ति माँगने ही को अपना व्यवसाय बना लेता है वह वास्तव में अपने लिए दरिद्रता का द्वार खोलता है।
तीसरी चीज़ जो अल्लाह को पसन्द नहीं है वह है धन का अपव्यय करना। अर्थात उसके व्यय में अनुत्तरदायित्वपूर्ण नीति अपनाना। धन अगर ग़लत और अनुचित जगहों पर ख़र्च किया गया तो उसे धन को नष्ट करना ही कहा जाएगा। इस्लाम में जिस प्रकार कृपणता बुरी है कि आदमी दौलत का पुजारी बनकर रह जाए और पैसा ख़र्च करते हुए उसके प्राण निकलने लगें उसी प्रकार धन का अपव्यय भी अपराध है। इसका अनुमान इस बात से भी किया जा सकता है कि हदीस में आया है कि अगर खाना खाते समय तुममें से किसी का कोई लुक़्मा गिर जाए तो उसको चाहिए कि उसे उठा ले और साफ़ करके खा ले, उसको शैतान के लिए न छोड़े (मुस्लिम)। इस्लाम को यह भी सहन नहीं कि भोजन का एक ग्रास भी नष्ट हो कि इससे शैतान के मिशन को बल मिलता है। इस्लाम ऐसा स्वभाव बनाता है कि मोमिनों के अन्दर एक ओर यह हौसला हो कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपना सब कुछ ईश्वर की राह में लुटा दें। दूसरी ओर एक पैसे का अपव्यय भी उनके लिए असहनीय हो। क़ुरआन में है— “निश्चय ही फ़ुज़ूलख़र्ची करनेवाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा ही कृतघ्न है।" (17:27)
कहाँ यह शिक्षा और कहाँ मुसलमानों की वर्तमान नीति। दोनों में कोई जोड़ नहीं। कितना ही धन ग़ैरइस्लामी समारोहों और विवाह आदि के ग़ैर-शरई रिवाजों में ख़र्च किया जाता है और हमें इसका आभास तक नहीं होता कि धन ईश्वर की अमानत है। अगर हम इसे ख़र्च करने का अधिकार रखते भी हैं तो इस प्रकार कि हम उसे उचित जगह पर ख़र्च करें। इसे नष्ट करने की छूट ईश्वर ने हमें नहीं दी है।
बिगाड़
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम अपने आप को दो आदमियों के मध्य बिगाड़ पैदा करने से बचाओ, क्योंकि यह आदत मूँडनेवाली (अर्थात धर्म और नैतिकता को तबाह करनेवाली) है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : लोगों के मध्य बिगाड़ पैदा करनेवाला अपने इस बुरे कृत्य से यह सिद्ध करता है कि वह अभी तक इस्लामी नैतिकता से बिल्कुल ही अपरिचित है। उसका ईमान और इस्लाम अभी तक उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं बन सका है। आदमी का धर्म और उसका ईमान जब तक उसका अपना चरित्र नहीं बन जाता वह परम्परा-मात्र और निष्प्राण होता है। ईमान जब अपनी मूल आत्मा से रिक्त हो जाए तो न वह दुनिया में उसके किसी काम का होता है और न आख़िरत में वह किसी को ईश्वर की पकड़ से बचा सकता है। यह एक तथ्य है कि लोगों के बीच सुलह के बजाए फूट और बिगाड़ को पसन्द करना आदमी की समस्त नेकियों पर पानी फेर देता है।
(2) हज़रत अबू-दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि रोज़े, सद्क़ा और नमाज़ से भी श्रेष्ठ क्या चीज़ है?” रावी का बयान है कि मैंने कहा कि क्यों नहीं, आप अवश्य बताएँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "वह है दो आदमियों के मध्य (जिनमें बिगाड़ पैदा हो गया हो) सुलह कराना। और एक-दूसरे के मध्य फूट डालना वह चीज़ है जो मूँड देनेवाली है।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : यह हदीस 'सामाजिक गुण' के अध्याय में हम पहले भी उद्धृत कर आए हैं। देखें शीर्षक 'परस्पर सुलह कराना'।
अध्याय-5
पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)
(1)
एक चरित्र नायक
आकर्षण
(1) हज़रत सईद जरीरी हज़रत अबू-तुफ़ैल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को देखा है। हज़रत सईद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि आपने उनको कैसा देखा? उन्होंने कहा कि आप गोरे थे, कुछ सलोनापन लिए हुए। जब चलते तो मानो ढलान में उतर रहे हों। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : एक रिवायत में है “इज़ा मशा य-त-कफ़्फ़ा" (शमाइले तिर्मिज़ी) अर्थात जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चलते तो आगे को झुके हुए चलते। इसके दो अनुवाद और भी किए जा सकते हैं। एक यह कि जब आप चलते तो तीव्र गति के साथ चलते। दूसरा अनुवाद ये हो सकता है कि जब आप चलते तो क़दम जमाकर चलते। वास्तव में ये तीनों ही अनुवाद सही हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चलने में तीनों ही प्रकार की विशिष्टताएँ पाई जाती थीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अहंकारियों कि भाँति सीना तानकर चलना पसन्द न था बल्कि नम्रता के कारण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) झुके हुए चलते। लेकिन आप सुस्त चाल न थे। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शक्ति के साथ पूरा पैर उठाकर आगे रखते थे। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ज़मीन पर पैर घसीट कर नहीं चलते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की चाल से हर कोई समझ सकता था कि यह कोई ज़िम्मेदार और सभ्य व्यक्ति गुज़र रहा है। यह न तो बेख़बर और अनुत्तरदायी हो सकता है और न यह अभिमानी और अहंकारी हो सकता है।
हदीस में ये शब्द आए हैं, "इज़ा मशा क-अन्नहू य-त-वक्का" जब चलते तो ऐसा प्रतीत होता कि आगे झुके जाते हैं।
(2) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) न तो बहुत लम्बे थे, न छोटे क़द के और न तो बिल्कुल श्वेत थे और न बिल्कुल गेहुँए रंग के। सिर के बाल न तो अधिक बल खाए हुए होते थे और न बिल्कुल सीधे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात प्रतापवान ईश्वर ने अपने रसूल को आन्तरिक और बाह्य दोनों पहलुओं से पूर्णता एवं सौन्दर्य प्रदान किया था। क़द आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का मध्यवर्ती था किन्तु सभाओं में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही उभरे हुए दिखाई देते। हदीसों से मालूम होता है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुखाकृति न लम्बी थी और न बहुत ज़्यादा गोल, बल्कि दोनों के मध्य थी। बाल न पेंचदार और घुँघराले थे और न बिल्कुल सीधे बल्कि किसी सीमा तक बल खाए हुए थे। आप का शरीर मोटा न था। आँखें सुरमई और पलकें लम्बी थीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की गरिमा ऐसी थी कि जो कोई सहसा आपको देखता आपके प्रभाव में आ जाता, वह आपके तेज और प्रताप के वशीभूत होकर रह जाता किन्तु आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निकट होकर आदमी आप पर मोहित होकर रह जाता।
(3) हज़रत बराअ् (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सब लोगों से अधिक सुन्दर और डील-डोल में सबसे बेहतर थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) न बहुत लम्बे थे और न छोटे क़द के थे। (हदीस : बुख़ारी)
वाणी और वाक्शैली
(1) हज़रत बराअ् (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इशा में सूरा “वत्तीनि वज़्ज़ैतून” पढ़ते हुए सुना। मैंने किसी को भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अधिक अच्छी आवाज़ का या क़ुरआन का अच्छा पाठ करनेवाला नहीं सुना। (हदीस : बुख़ारी)
(2) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब सलाम करते तो तीन बार करते और जब कोई बात कहते तो तीन बार कहते। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात आवश्यकता समझते तो बात को तीन बार दोहराते और तीनों ओर मुख करते ताकि सुननेवाले अच्छी तरह बात को समझ लें। और अगर समझते कि दो बार कहना ही पर्याप्त है तो दो ही बार कहते।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निवेदन किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! बहुदेववादियों को शाप दीजिए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि मुझे लानत करनेवाला बनाकर नहीं भेजा गया है। बल्कि मुझे तो सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा गया है। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मैं वह काम क्यों करूँ जो मेरे अवतरित होने का मूल उद्देश्य नहीं है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शाप देने से बचते थे। क्योंकि यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मर्यादानुकूल न था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों को बददुआएँ देते और उनपर लानत भेजते।
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) निरन्तर बात नहीं करते थे जिस प्रकार तुम लोग निरन्तर बोलते चले जाते हो। आप इस प्रकार ठहर-ठहरकर बात करते कि कोई गिननेवाला आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वाक्यों को गिनना चाहता तो गिन सकता था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ऐसा नहीं होता था कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लगातार बोलते चले जाएँ कि लोगों में उकताहट पैदा हो जाए। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तेज़ रफ़्तारी से बात नहीं करते थे कि सम्बोधित लोग कुछ बातें समझ सकें और कुछ न समझ सकें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अत्यन्त शान्तिपूर्वक बात करते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वाणी अत्यन्त स्वच्छ और सुस्पष्ट होती थी कि लोगों को उसके समझने में तनिक भी कठिनाई न हो। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वार्ता व्यर्थ की बातों से परे होती थी और उसमें वैसी त्रुटियाँ नहीं पाई जाती थीं जो साधारणतः लोगों की बात-चीत में पाई जाती हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वार्ताशैली आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की महानता और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के गरिमामयी व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण है।
अबू-दाऊद की एक हदीस में है—
"अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वाणी में प्रत्येक विषय सुस्पष्ट होता था कि हर श्रोता उसे समझ लेता।"
(5) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) न तो अश्लील बोलते थे, न धिक्कारते थे और न दुष्भाषी थे। जब किसी पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क्रोध आता तो बस इतना कहते “क्या हुआ उसे, धूलधूसरित हो उसका ललाट!” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मालूम हुआ कि आप अशिष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे अर्थात आप हमेशा सभ्य शब्दों का ही प्रयोग करते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वभाव धिक्कारनेवाला भी न था। मूल में “लअ्न" शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसके अर्थ हैं— हाँक देना, वंचित कर देना, अपमानित करना। धिक्कार शब्द जब ईश्वर की ओर से प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है "ईश्वर का किसी को अपने सामीप्य से दूर और अपनी अनुकम्पाओं से वंचित कर देना।" और जब इस शब्द का बन्दे की ओर से प्रयोग हो तो इससे अभिप्रेत है बुरा कहना और ईश्वरीय अनुकम्पा से दूर और वंचित होने का शाप देना। यही कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति को धिक्कारना जो धिक्कारने का पात्र न हो, सख़्त गुनाह की बात है।
“धूलधूसरित हो उसका ललाट" यह वाक्य किसी से अत्यन्त अप्रसन्नता और क्रोध की दशा में आप के मुख से निकलता था। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सीधे उस व्यक्ति को सम्बोधित न करके बात को परोक्ष रूप में रखते। आप कहते, "धूलधूसरित हो उसकी नाक" या “धूलधूसरित हो उसका ललाट”। इन वाक्यों में दो अर्थों की सम्भावना भी है। ये शब्द अपमान, अधमता और निम्नस्थता को भी इंगित कर सकते हैं किन्तु इन शब्दों को सज्दा करने के अर्थ में भी लिया जा सकता है। इस रूप में इन वाक्यों का अर्थ होगा, “ईश्वर तुझे अपने सम्मुख नतमस्तक होने का सौभाग्य प्रदान करे।" मानो क्रोधावस्था में भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से दुआ के शब्द ही निकलते थे।
(6) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-सलाम अपने पिता से उल्लेख करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब बातें करने बैठते तो बहुधा आपकी दृष्टि आसमान की ओर उठती रहती। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर की महानता और उसके प्रताप का बारम्बार स्मरण करते रहते। हदीस से ज्ञात होता है कि जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आकाश की ओर नज़र उठाते तो कहते, “ऐ हृदयों के फेरनेवाले, मेरे हृदय को अपनी आज्ञाकारिता पर जमाए रख।"
आकाश की ओर निगाह उठाने का एक और कारण यह भी वर्णित किया गया है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह ख़याल होता कि शायद जिब्रील वह्य लेकर आते हों।
(7) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल न तो स्वभाव से अश्लील-भाषी थे और न ही कृत्रिम रूप से आप अश्लील शब्दों का प्रयोग करते थे। और न बाज़ारों में शोर मचाते थे और न बुराई का बदला बुराई से लेते थे, बल्कि क्षमा कर देते और नज़रअन्दाज़ कर देते। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : सही बुख़ारी में है, "अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं अपने लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया।" मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप में कष्ट पहुँचने पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किसी से प्रतिशोध नहीं लिया। मक्का विजय के अवसर पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी जान के शत्रुओं को निस्संकोच क्षमा कर दिया। हालाँकि अगर आप चाहते तो अपने एक-एक दुश्मन से पूरा-पूरा बदला ले सकते थे। अलबत्ता शरई क़ानून की अवहेलना को आप कदापि सहन न करते। एक अवसर पर कहा, "ईश्वर की सौगन्ध, यदि मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके हाथ भी काट दूँगा।"
मुसकान
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कभी इस प्रकार हँसते नहीं देखा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सारा मुँह खुल गया हो और मुझे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कंठ की घाँटी नज़र आ गई हो। आपकी हँसी बस मुसकुराहट तक ही सीमित थी। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आम लोगों की भाँति ज़ोर से ठहाका लगाकर नहीं हँसते थे कि पूरा मुँह खुल जाए और अन्दर के मसूढ़े और गले की ग्रन्थि तक दिखाई देने लगे। प्रसन्नता और आनन्द के अवसर पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) केवल मुस्करा देने ही पर बस करते थे। कभी-कभी अगर हँसते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हँसी भी हल्की ही होती।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-हारिस-बिन-जज़इ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अधिक किसी और को मुस्कराते हुए नहीं देखा। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मतलब यह है कि आप शुष्क स्वभाव के न थे कि सदैव मुँह बिसूरे और शोकग्रस्त रहते। इस रूप में तो लोग आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकट आने से घबराते और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से दूर ही रहने को प्राथमिकता देते। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के व्यक्तित्व में तो वह आकर्षण था कि जो व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकट होता वह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर मोहित हो कर रह जाता। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अकसर मुस्कराते हुए ही देखते थे।
मौन (ख़ामोशी)
(1) हज़रत जाबिर-बिन-समुरह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अधिकतर ख़ामोश रहते थे। (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : मतलब यह है कि मौन और मितभाषिता नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रमुख गुण थे। अनावश्यक कभी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बात न करते। जब कोई आवश्यक बात करनी हो तो बोलते थे, अन्यथा ख़ामोश रहते थे। दूसरों के लिए भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यही निर्देश था कि—
"जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात मुख से निकाले अन्यथा चुप रहे।"
परहेज़गारी
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को रास्ते में एक खजूर (पड़ी हुई) मिली तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अगर मुझे इसका भय न होता कि कहीं यह सदक़े की न हो तो मैं इसको खा लेता।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात मुझे इसका संशय है कि कहीं यह खजूर सदक़े (दान) के खजूरों में से न हो जो ले जाते हुए किसी से गिर गई हो। इसलिए इसका खाना मेरे लिए वैध नहीं है। अन्यथा इसको उठाकर खा लेने में कोई बुराई न थी। आवश्यक नहीं कि यह खजूर सदक़े ही की हो लेकिन चूँकि इसके सदक़े की खजूर होने की सम्भावना पाई जाती है इसलिए एहतियात इसी में है कि मैं इसे न खाऊँ।
इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई ऐसी मामूली चीज़ रास्ते में गिरी हुई मिले जिसके गिरने का उसके मालिक को कोई ग़म नहीं होता और न किसी के उसको उठा लेने पर उसे कोई आपत्ति होती है तो उसको उठा लेने और अपने काम में लाने में कोई गुनाह नहीं।
अभिलाषा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि तुफ़ैल-बिन-अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क़बील-ए-दौस ने अवज्ञा की और इनकार किया, इसलिए आप उन्हें शापित करें। लोगों का विचार था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन लोगों को शापित करेंगे लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ अल्लाह, दौस को मार्गदशन प्रदान कर और उनको (मेरे पास) ला दे।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात तुझसे यह दुआ है कि क़बील-ए-दौस के लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो और वे तेरे वफ़ादार मुस्लिम बन जाएँ और मेरी अवज्ञा न करें।
नबियों की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि भटके हुए लोग संमार्ग पर आ जाएँ और मार्गदर्शन की निधि उनके भाग्य में आ जाए जो जीवन की सर्वाधिक बहुमूल्य निधि है। ईश्वर के बन्दों का कल्याण-भाव नबियों और पैग़म्बरों के हृदय में आत्यान्तिक रूप से पाया जाता है। और वास्तव में यह ईश्वर प्रेम ही की एक अपेक्षा होती है कि उसके बन्दों से भी हमें गहरा सम्बन्ध हो। उनसे प्रेम करें और उनकी शुभचिन्ता से कभी ग़ाफ़िल न हों।
व्यर्थ बातों से बचना
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर का स्मरण अधिक करते। व्यर्थ और अनावश्यक बातें न करते। नमाज़ को सुदीर्घ और अभिभाषण को संक्षिप्त करते। और विधवा और निर्धन के साथ चलने में वे लज्जा महसूस न करते और उसकी आवश्यकता पूरी कर देते थे। (हदीस : नसई, दारमी)
व्याख्या : “व्यर्थ और अनावश्यक बातें न करते", मूल में ‘युक़िल्लुल लग़्व’ आया है। अरबी में क़लील का शब्द बिल्कुल निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ क़ुरआन में है : “क़लीलम मा युअ्मिनून” अर्थात वे बिल्कुल ईमान नहीं रखते। कुछ टीकाकारों ने ‘युक़िल्लुल लग़्व’ का अनुवाद किया है— “आप व्यर्थ बातें बहुत कम करते थे।” व्यर्थ बातों से उनका तात्पर्य वे बातें हैं जिनका सम्बन्ध सांसारिक मामलों से हो। सांसारिक बातों से सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक बातों को व्यर्थ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ईश-स्मरण की तुलना में उपलक्ष्यतः उन्हें व्यर्थ कहा गया है। अन्यथा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से व्यर्थ बातें कभी निकली ही नहीं। स्वयं आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अनुयायियों तक की विशिष्टता क़ुरआन यह बताता है—
“जो व्यर्थ बातों से बचते हैं।" फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विषय में कोई व्यक्ति व्यर्थ बातों की कल्पना कैसे कर सकता है।
शील और स्वभाव
(1) हज़रत बराअ् (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सबसे अधिक सुन्दर और सबसे बढ़कर सुशील थे। न तो आप बहुत लम्बे क़द के थे और न आप छोटे क़द के थे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : मतलब यह है कि ईश्वर ने अपने रसूल को आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सदगुण प्रदान किए थे। मुखारविन्द की दृष्टि से ही आप सुन्दर न थे बल्कि इसके साथ ही शील-स्वभाव की दृष्टि से भी आप उच्च और श्रेष्ठ थे। क़ुरआन में भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—
“और निश्चय ही (ऐ नबी) तुम एक महान नैतिकता के शिखर पर हो।” (68:4)
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि—
“अल्लाह के नबी का शील क़ुरआन था।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क़ुरआन के अभीष्ट मानव का पूर्ण आदर्श थे। अर्थात क़ुरआन अपनी उच्च शिक्षाओं के द्वारा जिस प्रकार का इनसान बनाना चाहता है, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस पर पूरा उतरते थे। क़ुरआन में जो महान नैतिक शिक्षाएँ विद्यमान हैं उनको आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चरित्र और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)
वास्तव में क़ुरआन की शिक्षाओं का एक जीवन्त और पूर्ण आदर्श थे। क़ुरआन के रूप में न केवल यह कि ईश्वरीय आदेश क़ियामत तक के लिए सुरक्षित हो गए हैं बल्कि इसी के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पवित्र जीवनी भी इस किताब के द्वारा क़ियामत तक के लिए सुरक्षित हो गई है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन चरित्र पर लिखी हुई अन्य पुस्तकें यदि गुम भी हो जाएँ तब भी हम अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चरित्र और व्यक्तित्व को क़ुरआन में देख सकते हैं।
दृष्टि और विवेक
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह को हर समय याद करते थे। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ईश्वर से प्रत्येक समय और प्रत्येक अवस्था में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपना सम्बन्ध बनाए रखते थे। ईश्वर को प्रत्येक क्षण याद रखना इनसान के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उसका आध्यात्मिक आहार ही नहीं, उसकी शक्ति का मूल स्रोत भी है।
मानव एक संवेदनशील और सक्रिय अस्तित्व है। मानव की हैसियत कृषक और कर्मवीर की है। भोजन करना, कर्म और सक्रियता और संकल्प उसकी अनिवार्य विशेषता है। असम्भव है कि मानव कभी संकल्प और इरादे से रिक्त हो। इसलिए इनसान के लिए आवश्यक है कि उसका कोई इष्ट और प्रियतम हो जो उसके प्रेम और संकल्प का केन्द्र बिन्दु हो। इनसान के लिए सबसे बढ़ कर श्रेष्ठता की बात यह है कि उसका इष्ट ईश्वर हो। अगर वह ईश्वर से विमुख होता है तो अनिवार्यतः उसकी आसक्ति किसी और के प्रति होगी। इस प्रकार वह श्रेष्ठता और उच्चता के स्थान से गिर जाएगा।
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि मैंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप वित्र की नमाज़ पढ़ने से पूर्व सो जाते हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ आइशा, मेरी आँखें सोती हैं किन्तु मेरा हृदय नहीं सोता।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात सोने की दशा में भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ग़फ़लत से दूर रहते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आत्मा सोने की अवस्था में भी जाग्रत ही रहती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पवित्र हृदय पर भौतिकता का नहीं आध्यात्मिकता का वर्चस्व था। यही कारण है कि आपके दिल का चिराग़ सोने में भी रौशन रहता था।
(3) हज़रत जुन्दुब-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुझे ईश्वर के होते हुए यह स्वीकार नहीं कि तुममें से कोई मेरा ख़लील (प्रगाढ़ मित्र) हो। क्योंकि ईश्वर ने मुझे अपना ख़लील बना लिया है जैसे उसने इबराहीम को अपना ख़लील बनाया था।"
व्याख्या : ईश्वर के साथ बन्दे का आत्यन्तिक और प्रगाढ़ प्रेम 'ख़ुल्लत' कहलाता है। इसी प्रकार बन्दे के प्रति ईश्वर के प्रेमातिरेक को भी ख़ुल्लत कहते हैं। यह प्रेम वास्तव में ईश्वर की प्रभुता की अनिवार्यता है।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन का अर्थ यह है कि जब ईश्वर ने मुझे अपना ख़लील बनाया है तो वही मेरा भी ख़लील है। मेरे हृदय-राज्य पर वास्तव में उसी का आधिपत्य है। मैं उसके सामने बिछ गया हूँ और उसमें बिल्कुल खो गया हूँ। उसके प्रेम ने मेरे हृदय में घर कर लिया है।
ऐसा आत्यान्तिक प्रेम केवल एक ही के लिए हो सकता है। ख़ुल्लत में किसी की भागीदारी असम्भव होती है। किसी कवि ने कहा है—
“मेरी प्रिया मेरे भीतर आत्मा की भाँति व्याप्त है। इसी कारण ख़लील को ख़लील कहते हैं।"
(4) हज़रत मुग़ीरा-बिन-शोबा से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पाँवों में सूजन आ गई। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा गया कि आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं जबकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अगले और पिछले सब गुनाह क्षमा कर दिए गए हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या मैं ईश्वर का कृतज्ञ बन्दा न बनूँ!" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : "आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अगले और पिछले सब गुनाह क्षमा कर दिए गए हैं" यह संकेत क़ुरआन की इस आयत की ओर है—
"ऐ नबी, निश्चय ही हमने तुम्हें एक खुली विजय प्रदान की ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को क्षमा कर दे और तुमपर अपनी अनुकम्पा पूर्ण कर दे और तुम्हें सीधे मार्ग पर चलाए।” (48: 1-2)
“मैं ईश्वर का कृतज्ञ बन्दा न बनूँ" अर्थात इबादत का उद्देश्य केवल एक यही तो नहीं है कि हमारे गुनाह और त्रुटियाँ क्षमा हो जाएँ या ईश्वर की ओर से हमें किसी पकड़ और अज़ाब का संशय और भय न रहे। प्रणिपात और इबादत का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने उस प्रभु के प्रति कृतज्ञताप्रकाशन भी है जिसके हमपर अगणित उपकार हैं, जिसने हमारे अगले-पिछले समस्त गुनाह क्षमा कर दिए हैं। अपने प्रभु के उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि यह है कि हम कृतज्ञता के उत्कट भाव के साथ उसके आगे सज्दे में बिछ जाएँ।
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“दो रक्अतें फ़ज्र (प्रातः) की दुनिया और जो कुछ उसमें है, उससे बेहतर हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : एक रिवायत में है कि फ़ज़्र की दो रक्अतों के बारे में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“वे मुझे सारी दुनिया और उसकी चीज़ों से अधिक प्रिय हैं।”
(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “अगर मैं कहूँ 'सुबहानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर' तो यह मुझे उन सारी चीज़ों से प्रिय है जिनपर सूर्य उदय होता है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : ये शब्द जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सबसे प्रिय हैं उनका अर्थ है— महानता है अल्लाह के लिए, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई पूज्य प्रीतम नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है।
(7) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे वर्णन करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना कि—
“ईश्वर की सौगन्ध! मैं अल्लाह से दिन में सत्तर बार से अधिक क्षमा याचना करता हूँ और उसके आगे तौबा करता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात मैं रब के समक्ष बहुतायत से क्षमायाचना और तौबा करता रहता हूँ। मैं उसके दीन के लिए चाहे कितना ही क्यों न सक्रिय रहूँ उसकी बन्दगी का हक़ कहाँ अदा हो सकता है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए मैं क्षमाचायना और तौबा से काम लेता हूँ। मैं क्षमायाचना करता हूँ यह अभिलाषा लेकर कि मेरा प्रभु मेरी त्रुटियों और मेरे अवगुणों पर पर्दा डाल दे। वह मुझे अपनी रहमत से पूर्णतः ढाँक ले। इस प्रकार मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिट सकूँ ताकि मेरा प्रभु अधिक से अधिक उजागर हो सके।
मैं उसके समक्ष अधिकतर तौबा करता रहता हूँ। अर्थात मैं अधिकतर अपने प्रभु के उपकारों की आशा लिए हुए उसकी ओर उन्मुख होता हूँ। बारम्बार उसकी ओर पलटता हूँ ताकि उसकी अनुकम्पाओं और इनायतों से किसी पल भी वंचित न रहूँ। मेरा दिल ईश्वर के सिवा किसी दूसरी चीज़ में अपने लिए क़रार और चैन न खोज सके इसलिए भी मैं बार-बार अपने प्रभु की ओर पलटता हूँ।
(8) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब कोई हादसा पेश आता तो नमाज़ पढ़ने लग जाते थे। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इसलिए कि बन्दे के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका अपना प्रभु ही है। उसके सामीप्य से अच्छा कोई अन्य शरण स्थल नहीं हो सकता।
(9) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“स्वर्ग और इसी प्रकार नरक भी तुममें से हरेक की जूतियों के तस्मे से भी ज़्यादा उसके निकट है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात स्वर्ग और नरक को दूर न समझो। वह तो तुम्हारी जूतियों के तस्मों से भी अधिक तुमसे निकट हैं। स्वर्ग की नेमतें और उसकी सुख-सामग्रियाँ हों या नरक की विपत्तियाँ और कष्ट, उनका हमारे कर्मों और विचारों से गहरा सम्बन्ध है। हमारे कर्म और विचार ही होंगे जिनके कारण हमारा जीवन स्वर्गिक जीवन में बदल जाएगा या वह नरक के जीवन का रूप ले लेगा। हमारे कर्म हमसे दूर या हमसे अलग नहीं होते। कर्मों के द्वारा स्वयं हमारा अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व प्रकट होता है। कर्म यदि अच्छे और ईश-परायणता पर आधारित हैं तो हमारी जन्नत हमसे कुछ भी दूर नहीं है और अगर इसके विपरीत हमारे चरित्र और कर्म इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हम अपने प्रभु को ग़ैर समझते हैं और वह रास्ता अपना रखा है जो हमारे प्रभु को प्रिय नहीं, तो समझ लीजिए कि स्वर्ग के बजाए हम नरक से अपना गहरा रिश्ता और सम्बन्ध स्थापित कर चुके हैं।
(10) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बोरिए पर सोए। उठे तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शरीर पर बोरिए के निशान पड़े हुए थे। इब्ने-मसऊद ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें आदेश देते तो हम आप के लिए फ़र्श बिछाते और अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर देते। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"मुझे इस दुनिया से और इस दुनिया को मुझसे क्या सरोकार? मेरी और इस दुनिया की मिसाल तो बस ऐसी है जैसे कोई सवार किसी वृक्ष के नीचे छाया की तलाश में आए और फिर उसे छोड़ कर चल दे।” (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)
व्याख्या : अर्थात वास्तव में मेरे झुकाव और अभिरुचि का केन्द्र दुनिया और उसका आराम नहीं है बल्कि मेरे सामने तो आख़िरत की दुनिया है। जिस प्रकार एक सवार अपनी यात्रा तय करते हुए किसी वृक्ष के नीचे छाया के लिए अपने घोड़े को रोककर फिर आगे बढ़ जाता है ठीक उसी प्रकार मेरे समक्ष आख़िरत का सफ़र है। फिर मैं किसी ऐसी चीज़ को कैसे महत्व दे सकता हूँ और उसकी ओर कैसे झुक सकता हूँ जो आख़िरत की चिन्ता से मुझे ग़ाफ़िल कर सकती है।
(11) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक बार हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ थे कि वर्षा होने लगी। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपना कपड़ा उतार लिया, यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ऊपर बारिश का पानी गिरने लगा। हमने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा क्यों किया? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इसलिए कि बारिश का यह पानी अभी ताज़ादम अपने रब के पास से आया है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : “अपना कपड़ा हटा दिया" अर्थात अपने सिर या पीठ से कपड़ा हटा दिया। यह हदीस बताती है कि बन्दे को अपने प्रभु की अनुकम्पाओं के सिलसिले में कितना संवेदनशील होना चाहिए। यह हमारे भक्तिभाव की अपेक्षा है कि ईश्वर की अनुकम्पाओं के सम्बन्ध में हम अत्यन्त संवेदनशील हों। हमारे लिए आवश्यक है कि प्रभु की हर ताज़ा अनुकम्पा हमारे एहसास और ईमान को भी ताज़ा कर दे। और हमारी ओर से इस बात की अभिव्यक्ति हो कि हम अपने प्रभु की अनुकम्पाओं के प्रत्याशी हैं। हम कभी और किसी हालत में भी उसकी कृपादृष्टि की उपेक्षा नहीं कर सकते।
पानी की जो बूँद ईश्वरीय योजना से बारिश के रूप में गिरती हैं उसके और ईश्वर के बीच कोई प्रविष्ट नहीं होता। मानो उसका ईश्वर से सीधा सम्पर्क होता है। वह मासूम बूँद सर्वथा पवित्र होती है। ईश्वर-द्रोहियों और अवज्ञाकारी लोगों के अपवित्र हाथ अभी उस तक पहुँचे हुए नहीं होते। इसलिए पानी के ऐसे क़तरे बड़ी बरकत के होते हैं। इसलिए उनको अपने शरीर पर लेना एक अच्छे मनोभाव और एक शुभ इच्छा को व्यक्त करना है।।
(12) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा किसी व्यक्ति को धर्म के अतिरिक्त किसी और चीज़ से सम्बन्ध सम्बद्ध करते नहीं सुना। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात प्रत्येक काम में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) धार्मिक भावना को दृष्टि में रखते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दृष्टि में धर्म के महात्म की अपेक्षा हर चीज़ तुच्छ थी। अतएव रंग और वंश आदि की अपेक्षा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के यहाँ प्राथमिकता हमेशा धर्म ही को प्राप्त रहती थी। जो व्यक्ति धर्म में श्रेष्ठ होता उसे दूसरों पर प्राथमिकता देते चाहे वह किसी भी परिवार या क़बीले का क्यों न हो।
अभिरुचि
(1) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"तुम बढ़ा-चढ़ाकर मेरी प्रशंसा न करो जैसा कि ईसाइयों ने मरयम के बेटे की प्रशंसा में अतिशयोक्ति से काम लिया। मैं तो बस अल्लाह का बन्दा हूँ। अतः तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल कहा करो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात पद-प्रतिष्ठा आदि के अन्तर को दृष्टि में रखना आवश्यक है। आम तौर पर लोग अपने बड़ों की प्रशंसा में अतिशयोक्ति से काम लेते हैं। अतएव ईसा मसीह के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का बेटा घोषित कर दिया। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को ईश्वर का पुत्र कहा। हालाँकि ईश्वर के ईश्वरत्व में कोई भी शरीक नहीं हो सकता। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी प्रशंसा में अतिशयोक्ति से काम लेने से रोका। बन्दगी को रिसालत के साथ सम्मिलित किया। साक्ष्य वाक्य (कलिमा शहादत) अर्थात "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह एक है, उसका कोई साझीदार नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।" इस वाक्य में ‘अब्दुहू व रसूलुहु' (उसके बन्दे और उसके रसूल) के शब्द भी सम्मिलित हैं ताकि यह हमेशा स्मरण रहे कि रसूल या पैग़म्बर भी अल्लाह का एक बन्दा ही होता है, यद्यपि वह श्रेष्ठ और पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति होता है। इस प्रकार इस्लाम ने शिर्क की जड़ सदा के लिए काट दी है।
(2) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे सहाबा में से कोई मुझ तक किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई बुरी बात न पहुँचाए क्योंकि मैं यह पसन्द करता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा सीना (हृदय) साफ़ हो।”
(हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात कोई व्यक्ति किसी के बारे में मुझसे कोई बात कहकर मुझे उसके सम्बन्ध में बदगुमान करने का प्रयास न करे। अगर किसी साथी के अन्दर कोई कमज़ोरी तुम्हें महसूस हो तो हमदर्दी और सहानुभुति यह होगी कि अकेले में उसे इसका ध्यान दिलाओ, न कि बुराई को फैलाते फिरो। मैं चाहता हूँ कि तुमसे मिलूँ तो मेरे दिल में किसी व्यक्ति के बारे में अप्रसन्नता और नाराज़गी की भावना न हो।
किसी के मामले को आगे बढ़ाने और उसको ज़िम्मेदारों और प्रभावी लोगों के समक्ष रखने का मामला सबसे अन्त में आता है जब सुधार के समस्त प्रयास निष्फल सिद्ध हो रहे हों और मामला भी ऐसा हो कि उसे अनदेखा करने से किसी बड़े फ़ित्ने और बिगाड़ की आशंका पाई जाती हो।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं कदापि इस बात को पसन्द नहीं करता कि किसी की नक़्ल उतारूँ यद्यपि मेरे लिए ऐसा और ऐसा हो।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं कि किसी व्यक्ति की नक़्ल उतारूँ चाहे वह नक़्ल मौखिक हो या शारीरिक, और यद्यपि इससे कितने ही सांसारिक और भौतिक फ़ायदों की सम्भावना क्यों न हो।
(2)
प्रशंसनीय गुण
मनुष्य होने का एहसास
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी भूलता हूँ जिस तरह तुम लोग भूलते हो। अतएव जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ज़ुहर की नमाज़ में चार रक्अतों के स्थान पर पाँच रक्अतें अदा कीं। सहाबा ने कहा कि क्या नमाज़ में अभिवृद्धि हुई है? (इसलिए कि नमाज़ में चार ही रक्अतें अनिवार्य हैं।) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सहव (भूल) के दो सज्दे किए और वह बात कही जो इस हदीस में वर्णित है कि मैं भी मनुष्य हूँ, भूल सकता हूँ। भूलना तो मनुष्य की वृत्ति है। अगर मैं कभी भूलूँ तो तुम मुझे याद दिला दो।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ अल्लाह मैं मनुष्य हूँ, अतः जिस मुसलमान व्यक्ति को मैं बुरा कहूँ या उसपर लानत करूँ या उसे मारूँ तो तू इसे उसके लिए उत्कृष्टता का साधन बना और उसपर दया दर्शा।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मनुष्य होने के नाते नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क्रोध भी आता था लेकिन यह दयालुता की पराकाष्ठा है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाह से दुआ की कि अगर मैं किसी मुसलमान को बुरा कहूँ, उसे मारूँ या लानत करूँ तो इसे उसके लिए अपनी दया का निमित्त बना और उसे उत्कृष्टता प्रदान कर।
एक रिवायत में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते थे—
“ऐ अल्लाह, मैं जिस मोमिन बन्दे को बुरा कहूँ तू क़ियामत के दिन इसे उसके लिए अपने सामीप्य का साधन बना।" (हदीस : मुस्लिम)
एक हदीस में है—
“अर्थात इसे उसके लिए उसके गुनाहों का प्रायश्चित बना दे।” (हदीस : मुस्लिम)
(3) हज़रत उम्मुल-अला (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ईश्वर की सौगन्ध, मुझे नहीं मालूम कि (अल्लाह के यहाँ) मेरे साथ क्या मामला होगा, हालाँकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।” (हदीसः बुख़ारी)
व्याख्या : यह एक लम्बी हदीस का एक अंश है। हज़रत उसमान-बिन-मज़ऊन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के निधन पर हज़रत उम्मुल-अला (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने उन्हें सम्बोधित करके कहा कि ऐ अबू-साएब, तुम पर अल्लाह की कृपा हो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें अनुगृहीत किया है। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अनुगृहीत किया है? हज़रत उम्मुल-अला (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने कहा कि मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों, मैं नहीं जानती कि (उनपर नवाज़िश न होगी) तो कौन है जिसपर अनुग्रह होगा? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि उसमान तो जा चुके हैं, उनके बारे में अच्छी उम्मीदें मैं भी रखता हूँ। और फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वह बात कही जो मैंने यहाँ उद्धृत की है कि “ईश्वर की सौगन्ध स्वयं मुझे नहीं ज्ञात कि मेरे साथ क्या मामला पेश आएगा जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।" मतलब यह है कि अल्लाह के प्रताप और उसकी महानता का तक़ाज़ा है कि हम उससे डरते रहें और उसके प्रकोप और उसकी पकड़ के सिलसिले में किसी भी हालत में निश्चिन्त न रहें। हाँ, ईश्वर से अच्छी उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन निश्चयपूर्वक किसी के सम्बन्ध में कोई बात कहनी सही नहीं है।
विनम्रता और भक्तिभाव
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते थे—
“अल्लाह के सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, वह एक है, उसने अपनी सेना को प्रभावी किया और अपने बन्दे की सहायता की, और अधर्मियों के दल को पराभूत किया। वह एक है। उसके बाद कोई वस्तु नहीं।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : स्पष्ट है कि ये शब्द आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से उस समय निकले होंगे जब मोमिनों को अधर्मियों पर विजय प्राप्त हुई होगी और विधर्मियों को पराजय का मुँह देखना पड़ा होगा। इस विजय और सफलता पर बजाय इसके कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) गर्व करते और उसे अपना कारनामा समझते इस सफलता को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर की कृपा और उसका उपकार घोषित करते हैं और ईमानवालों की सेना को अपनी सेना कहने के बजाय उसे अल्लाह की सेना कहकर पुकारते हैं। और स्वयं को ईश्वर का एक बन्दा और विनीत दास समझते हैं।
"वह एक है, उसके बाद कोई वस्तु नहीं।" मतलब यह है कि एक ईश्वर के बाद कुछ नहीं बचता कि वह हमारी सम्बद्धता का केन्द्र बन सके। ईश्वर के सिवा जो कुछ है वह कुछ न होने का पर्याय है। इसी तथ्य को क़ुरआन ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, "ईश्वर के मुखारविन्द के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु नष्टप्राय है।"
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना—
“किसी व्यक्ति को उसका कर्म स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं कराएगा।" लोगों ने पूछा कि क्या आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल? कहा, “नहीं, मुझे भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह मुझे अपनी अनुकम्पा और दयालुता से ढाँक ले। अतएव तुम सुदृढ़ता और सुनीति अपनाओ और सामीप्य बनाए रखो और तुममें से कोई मृत्यु की कामना न करे। इसलिए कि वह या तो सुकर्मी होगा तो इस स्थिति में आशा है कि वह नेकियों में वृद्धि करे और अगर वह बुरा है तो कदाचित वह (तौबा करके) ईश्वर को प्रसन्न कर ले।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक हदीस में है—
“जान रखो कि तुममें से कोई व्यक्ति अपने कर्म के कारण मुक्ति नहीं पाएगा।"
क़ुरआन में है—
“और उन्हें आवाज़ दी जाएगी यह स्वर्ग है, जिसके तुम वारिस बनाए गए, उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे थे।" (7:43)
क़ुरआन और हदीस के बयान में वास्तव में कोई विसंगति नहीं पाई जाती। स्वर्ग का महान उत्तराधिकार तो ईश्वरीय अनुकम्पा और अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। इनसान के सत्कर्म तो मात्र निमित्त होंगे। सत्कर्म से केवल इस बात की आशा की जा सकती है कि ईश्वर दया करेगा। स्वर्ग में प्रवेश का वास्तविक कारण ईश्वरीय अनुग्रह के सिवा और कुछ नहीं। उसकी कृपा साथ न दे तो इनसानी कर्मों की हैसियत कुछ भी नहीं हो सकती।
अल्लाह किसी जीव पर बस उसकी सामर्थ्य और समाई के अनुसार ही दायित्व का भार डालता है (क़ुरआन 2:286)। इसलिए सुनीति और सुदृढ़ता अपनाओ किन्तु मध्यमार्ग को सदैव दृष्टि में रखो ताकि सन्तुलित मार्ग पर सदैव गमन करना तुम्हारे लिए सम्भव हो सके। अगर अपने ऊपर सख़्ती करते हो तो यह सख़्ती देर तक चलने की नहीं है। इसकी आशंका है कि सिरे से कर्म ही न छूट जाए। यह बात याद रहे कि “अल्प, जो शेष रहे वह, उस अधिक से उत्तम है जो शेष न रहे।"
सद्दाद कहते हैं कि सुदृढ़ता और अनुसरण और सामीप्य उस मध्यमार्ग को कहते हैं जिसमें न तो अतिशयता से काम लिया गया हो, न अत्यल्पता से।
किसी व्यक्ति को अगर सत्कर्म का सुअवसर न प्राप्त हो रहा हो तब भी उसे मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए। जीवन में इसकी सम्भावना है कि उसको तौबा का सुअवसर प्राप्त हो और उसपर से ईश्वरीय प्रकोप दूर हो जाए।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) वर्णन करती हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को, इस हाल में कि आप मुझ पर सहारा लगाए हुए थे, यह कहते हुए सुना कि—
“ऐ अल्लाह मुझे क्षमा कर दे और मुझपर दया कर और मुझे रफ़ीक़ (जगत-सखा) से मिला दे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : जीवन भर ईश्वरीय मार्ग में सक्रिय रहने के बाद भी अपने ईश्वर से क्षमादान और अनुकम्पा की याचना कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं तो इसकी कि जीवन सखा से मिलन हो। यही विनम्रता और भक्तिभाव है जो ईमान की वास्तविक आत्मा और हृदय एवं प्राण का सौन्दर्य है।
(4) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस्तिस्क़ा (अर्थात बारिश की दुआ) के लिए निकले। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कैफ़ियत यह थी कि साज-सज्जा रहित, विनम्र, विनीत और (ईश्वर के समक्ष) गिड़गिड़ानेवाले थे।
व्याख्या : अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुद्रा से विनम्रता और विनीतभाव प्रकट था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से रुदन और द्रवणशीलता का भाव भी प्रकट हो रहा था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पानी के लिए दुआ करने बाहर निकले थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस बात को भली-भाँति समझते थे कि ईश्वरीय अनुकम्पा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, चाहे वह अनुकम्पा वर्षा के रूप में हो या किसी और रूप में, आवश्यक है कि बन्दा अपने प्रभु के आगे विनीत भाव से आवश्यकता प्रदर्शित करे। आदमी को यूँ तो हर समय और हर हालत में एक विनीत और मुहताज बन्दा बनकर रहना चाहिए लेकिन विपत्ति के अवसर पर तो अनिवार्यतः उसे अपनी विवशता और मुहताजी का पूरा एहसास होना चाहिए। बन्दे के शरीर पर जो वस्त्र शोभा देता है वह केवल विनयशीलता का वस्त्र है, न कि कोई और वस्त्र। ईश्वर का पैग़म्बर हमारे अन्दर इसी भाव को अपने व्यवहार और अपनी शिक्षाओं के द्वारा जगाना चाहता है।
(5) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बद्र के युद्ध के अवसर पर एक ख़ेमे में यह दुआ माँग रहे थे—
“ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे प्रश्रय की याचना करता हूँ और चाहता हूँ कि तेरा वादा और वचन पूरा हो ऐ अल्लाह, अगर तू यही चाहता है कि (मुसलमान हलाक हो जाएं) तो आज के बाद फिर तेरी इबादत न होगी।" इसपर अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हाथ पकड़ लिया और निवेदन किया कि "ऐ अल्लाह के रसूल, बस इतना पर्याप्त है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुत द्रवणशीलता और रुदनभाव के साथ अपने प्रभु से विनती की है।" इसके बाद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कवच पहने हुए तेज़ी से बाहर आए। और आप यह आयत पढ़ रहे थे, “अधर्मियों का यह दल जल्द ही पराजित होगा और वे पीठ फेरकर भाग खड़े होंगे।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ईश्वर ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को वचन दिया था कि—
"और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दो गरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आएगा" (क़ुरआन, 8:7)
अल्लाह के इस वादे का हवाला देकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दुआ कर रहे थे। अल्लाह के वादे पर विश्वास के बावजूद बन्दे का कर्तव्य है कि वह अपने प्रभु से प्रार्थना और विनयपूर्वक याचना करने में कोताही न करे। बन्दे की दासता और ईश्वर की महानता की माँग भी यही है कि बन्दा अत्यन्त द्रवितभाव के साथ उससे दुआएँ करता रहे। इस दुआ से इस्लामी मुजाहिदों के दिलों को बल देना और उनका उत्साहवर्द्धन भी एक विशेष प्रयोजन हो सकता है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कवच पहने हुए बाहर आए तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़बान पर क़ुरआन की वह आयत थी जिसका उल्लेख इस हदीस में किया गया है। इस आयत के द्वारा मानो आप ईमानवालों को ईश्वर की ओर से शुभ सूचना दे रहे थे कि शत्रुओं के मुक़ाबले में विजय मुसलमानों ही को प्राप्त होगी।
ईशभय
(1) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं क्योंकर सुख और आनन्द का उपभोग करूँ जबकि वस्तुस्थिति यह है कि सूर फूँकनेवाले फ़रिश्ते ने सूर (नरसिंघा) को अपने मुँह में ले लिया है, अपना माथा झुका लिया है और अपने कान लगा रखे हैं और इस प्रतीक्षा में है कि उसे सूर फूँकने का आदेश मिले।” सहाबा ने कहा कि इस अवस्था में आप हमें क्या आदेश करते हैं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "कहो : हमारे लिए अल्लाह पर्याप्त है और वह बेहतरीन कार्यसाधक है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात जिस किसी व्यक्ति को भी इस स्थिति की गम्भीरता की अनुभूति होगी कि फ़रिश्ता सूर में फूँक मारने को बिल्कुल तैयार है, किसी समय भी क़ियामत आ सकती है, वह चैनपूर्वक कैसे रह सकता है। और संसार का कोई भी सुख और आराम उसे इस परिस्थिति से कैसे निश्चिंत रख सकता है। उसको यही चिन्ता घेरे रहेगी कि संसार में उसके जीवन का कोई क्षण भी यूँ ही व्यतीत न हो जाए, बल्कि वह ईश्वर से सदैव डरता रहे।
इनसान जिस परिस्थिति से दोचार है अगर उसे उसकी गम्भीरता का आभास हो तो उसे कदापि चैन नहीं मिल सकता। ऐसी हालत में इनसान के लिए सही कार्यनीति अगर हो सकती है तो वह यही है कि वह ईश्वर की अवज्ञा और गुनाहों से बचता रहे और उसकी बन्दगी की कभी उपेक्षा न करे, लेकिन असली भरोसा उसे अपने अमल पर नहीं बल्कि अपने ईश्वर पर हो। किसी पर अगर भरोसा और विश्वास किया जा सकता है तो वह कोई और चीज़ नहीं बल्कि ईश्वर ही है। आदमी ईश्वर ही को अपना कार्यसाधक समझे और अपना मामला उसके हवाले कर दे और कहे कि अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है। परेशानियों में इसी से उसे शान्ति मिल सकती है।
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मैंने कभी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस प्रकार हँसते नहीं देखा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की घाँटी नज़र आई हो। आप केवल मुस्कराते थे। और जब बादल या हवा को देखते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चेहरे की मुद्रा बदल जाती जिसे सरलतापूर्वक भाँपा जा सकता था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चेहरे से भय के लक्षण स्पष्ट दीख पड़ते थे। यूँ तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हृदय ईश-भय से किसी भी समय रिक्त न रहता था। किन्तु बादलों के छा जाने और हवा के चलने पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ज़्यादा चिन्तित हो जाया करते थे कि कहीं बादल और हवा के पीछे ईश्वरीय प्रकोप की बिजलियाँ न छिपी हों। एक हदीस से ज्ञात होता है कि ऐसी परिस्थति में आपकी चिन्ता और घबराहट इतनी बढ़ जाती थी कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) व्याकुल हो कभी घर से बाहर आते और कभी घर के अन्दर जाते। यह व्याकुलता उस समय समाप्त होती जब वर्षा होने लगती। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से आपकी घबराहट के विषय में पूछा तो कहा—
“आइशा, क्या ख़बर, ये बादल वैसे ही न हों जिसके सम्बन्ध में आद की क़ौम ने कहा था : यह बादल है, हमपर बरसेगा।"
अर्थात आद के लोग भ्रम में रहे। ईश्वर ने उन्हें विनष्ट करके शीघ्र ही उनके इस भ्रम को दूर कर दिया।
(3) हज़रत मुतरिफ़-बिन-अब्दुल्लाह-बिन-शिख़्ख़ीर (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ, उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नमाज़ पढ़ रहे थे और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सीने से इस तरह आवाज़ निकल रही थी जैसे किसी पकती हाँडी से आवाज़ निकलती है अर्थात आप रो रहे थे। (हदीस : मुस्नद अहमद, नसई)
व्याख्या : अबू-दाऊद की हदीस में है—
“मैंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नमाज़ पढ़ते देखा। उस समय रोने के कारण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सीने से चक्की की-सी आवाज़ आ रही थी।"
नमाज़ में ईशभय के कारण रोने और आह करने से नमाज़ व्यर्थ नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा और कष्ट के कारण आह करे और ऊँची आवाज़ में रोए तो उसकी नमाज़ टूट जाएगी। (हदीस : हिदाया)
(4) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मैं एक रात अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बिस्तर पर न पाकर आपको तलाश करने लगी। मेरा हाथ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के तलवे पर पड़ा। आप सज्दे में थे और दोनों पाँव उठे हुए थे। और आप कह रहे थे—
“ऐ अल्लाह मैं तेरे प्रकोप से बचने के लिए तेरी प्रसन्नता का आश्रय लेता हूँ। तेरी यातना से सुरक्षित रहने के लिए तेरे क्षमादान और तेरी पकड़ से बचने के लिए तेरी ही शरण लेता हूँ। मुझमें यह सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरी पूर्ण स्तुति कर सकूँ। तू ऐसा ही है जैसा कि तूने स्वयं अपनी प्रशंसा की है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दुआ के ये शब्द यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पवित्र हृदय किन भावों से परिपूर्ण था और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईशभय से कितना अधिक डरे रहते थे।
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब लोगों को आदेश देते तो उन्हें उन कर्मों को करने का आदेश देते जिन्हें करने की उनमें शक्ति होती। लोगों ने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जैसे कदापि नहीं। अल्लाह ने तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अगले और पिछले समस्त गुनाहों को क्षमा कर दिया है। इसपर आप अत्यन्त क्रुद्ध हुए यहाँ तक कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चेहरे पर क्रोध का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर आप ने कहा—
“मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह का डर रखता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला मैं हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक हदीस में है—
“मैं सब लोगों से अधिक अल्लाह को जानता हूँ और सबसे बढ़कर उससे डरता हूँ।"
हदीस का अर्थ यह है कि ईश्वर के आज्ञापालन और उपासना का वास्तविक प्रेरक ईश्वर की पहचान और उसका भय है। इससे हटकर किसी दूसरी चीज़ को इसका प्रेरक समझना सही नहीं। जब ईश-ज्ञान और ईशभय में मैं तुम सबसे बढ़कर हूँ तो फिर ईश-आज्ञापालन और उपासना में तुम्हें मेरा अनुसरण करना चाहिए। मेरे तरीक़े से हटकर जो भी तरीक़ा तुम अपनाओगे वह ग़लत और ईश्वरीय मंशा के विरुद्ध होगा।
ईश्वर को जानने और ईशभय को धारण करने में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी एक और विशिष्टता यह बताई है कि अमानत की अदायगी में भी दूसरा कोई आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का मुक़ाबला नहीं कर सकता। अतएव एक यहूदी ने द्वेष और शत्रुता के कारण दरपरदा जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की अमानतदारी पर शंका प्रकट की तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"वह झूठा है और वह स्वयं यह जानता है कि मैं तमाम लोगों से अधिक ईश्वर से डरनेवाला और उनसे बढ़कर अमानतों को अच्छी तरह अदा करनेवाला हूँ।"
कृतज्ञता
(1) हज़रत मुग़ीरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने रात में इतना दीर्घ क़ियाम किया कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पैरों में सूजन आ गई। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपके तो सब अगले पिछले गुनाह क्षमा हो चुके हैं? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"क्या मैं एक कृतज्ञ बन्दा न बनूँ?” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, इब्ने-माजा)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने देर तक नमाज़ में क़ियाम किया यहाँ तक कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पैरों में सूजन आ गई। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इबादत में असाधारण श्रम से काम लेते थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा गया कि आप अपने को इतनी कठिनाई में क्यों डालते हैं? नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो श्रम कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता तो महसूस नहीं होती। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तो सब अगली-पिछली कोताहियाँ क्षमा कर दी गई हैं। यह बात सम्भवतः क़ुरआन की सूरा अल-फ़त्ह, आयत-2 के अन्तर्गत कही।
इस प्रश्न का नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो उत्तर दिया उसका अर्थ यह है कि जब ईश्वर ने मुझपर असीम उपकार किया है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसका कृतज्ञ बन्दा बनूँ और अधिक से अधिक उसकी प्रसन्नता का इच्छुक रहूँ।
इस हदीस से मालूम हुआ कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने की एक अपेक्षा यह है कि बन्दा ईश्वर के साथ अधिक से अधिक अपने सम्बन्ध को व्यक्त करे, और अधिक से अधिक उसके सामीप्य का इच्छुक हो। और इसका सर्वोत्तम साधन नमाज़ है। और सज्दा तो विशेष रूप से सामीप्य का साधन है बल्कि सामीप्य की अवस्था ही का दूसरा नाम है।
धैर्य
(1) हज़रत जुंदुब-बिन-सुफ़ियान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि किसी लड़ाई में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की अंगुली जख़्मी हुई और ख़ून निकल आया तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (अपनी अंगुली को सम्बोधित करते हुए) कहा—
“तू मात्र एक रक्त रंजित अंगुली है। तुझे जो मुसीबत पहुँची है वह ईश्वरीय मार्ग में पहुँची है।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात जब यह कष्ट ईश्वरीय मार्ग में पहुँचा है तो इसपर मुझे खेद क्यों हो। ईश्वरीय मार्ग में तो प्राण तक वारे जा सकते हैं। ईश्वरीय मार्ग पर गमन करनेवालों के मार्ग को विपत्तियाँ रोक नहीं सकतीं। और न ईश्वरीय मार्ग के यात्री इस मार्ग में पहुँचनेवाले कष्टों की किसी से शिकायत करते हैं।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैं मानो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को एक नबी का वृत्तांत सुनाते देख रहा हूँ जिनको उनकी क़ौम ने मारा था। वह अपने चेहरे से रक्त पोंछते जाते थे और कहते जाते थे—
“ऐ अल्लाह, तू मेरे लोगों को क्षमा कर दे क्योंकि वे जानते नहीं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : वास्तव में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वयं अपना भी यही वृत्तांत है। क़ौम के हाथों आप भी तायफ़ के दावती सफ़र में और उहुद के युद्ध में ज़ख़्मी हुए थे। लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने असाधारण धैर्य से काम लिया। पर्वतों के फ़रिश्ते ने जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि आप कहें तो मैं दोनों पर्वतों (अबू-क़बीस और औस के सामने का पर्वत जो मक्का में है) उन लोगों पर उलट दूँ (और ये लोग पिस जाएँ) तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जवाब में कहा—
“नहीं, बल्कि मैं आशा रखता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्ल से उन लोगों को पैदा करेगा जो एक ईश्वर की उपासना करेंगे और किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहराएँगे।" (हदीस : मुस्लिम, बुख़ारी, नसाई)
शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मानसिक कष्ट भी सहन किए हैं। एक बार जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कह रहा है कि माल के बँटवारे में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ईश्वर और अन्तिम दिन को दृष्टि में न रखा तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह की रहमत हो मूसा (अलैहिस्सलाम) पर, उनको इससे अधिक कष्ट पहुँचाए गए और उन्होंने सब्र किया।" (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)
सादगी
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक पुराने कजावे पर फटी-पुरानी चादर में हज किया जिसका मूल्य चार दिरहम रहा होगा या चार दिरहम भी न रहा होगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : जिस प्रकार से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने अनुयायियों को सादगी की शिक्षा दी है उसी प्रकार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं भी सादगी को अपनाया और सांसारिक साज-सज्जा की आपको कोई परवाह न हुई। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यह सादगी उस ज़माने की है जबकि सम्पूर्ण अरब इस्लाम के अधीन था। यह 10 हिजरी की बात है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ सामान और असबाब अर्जित कर सकते थे।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक चटाई पर सोए। जब आप उठे तो चटाई के निशान आप के पहलू पर उभरे हुए थे। हमने निवेदन किया कि क्या अच्छा हो कि हम आपके लिए एक तोशक बना दें। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुझे दुनिया से क्या मतलब? मैं तो इस दुनिया में बस उस यात्री की भाँति हूँ जो किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी छाया ले और फिर उसे छोड़कर (आगे अपने गन्तव्य की ओर) प्रस्थान करे।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी व्यवहार-नीति से यह व्यक्त किया कि संसार इसलिए नहीं है कि कोई इसकी चाह में जिए और मरे। संसार तो मात्र एक मार्ग है, उसे ही गन्तव्य समझ लेने की ग़लती कदापि नहीं करनी चाहिए।
यह दृष्टि में रहे कि बोरिये पर सोने की यह घटना जो इस हदीस में वर्णित है, उस समय की है जब इस्लाम सत्ता में था।
यह एक वास्तविकता है कि दुनिया से जो व्यक्ति भी प्रेम करेगा आख़िरत का महत्व और उसका मूल्य उसकी दृष्टि में शेष नहीं रह सकता। इसलिए दृष्टि हमेशा आख़िरत पर होनी चाहिए। संसार में अगर चिन्ता हो तो केवल अपने दायित्वों के निर्वहण की।
गुनाहों से बचना
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दो कामों में किसी एक को करने का विकल्प दिया जाता तो अनिवार्यतः नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनमें से जो आसान होता उसे अपनाते। बस शर्त यह थी कि वह गुनाह न हो। अगर वह गुनाह (का कारण) होता तो लोगों में सबसे बढ़कर आप उससे दूर रहनेवाले थे। और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं अपने लिए कभी (किसी से) प्रतिशोध नहीं लिया। अलबत्ता अल्लाह की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई काम किया जाता तो आप अल्लाह के लिए अवश्य उसका प्रतिशोध लेते। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : धर्म में यह कदापि अपेक्षित नहीं कि आदमी अनिवार्यतः अपने आप को कष्ट में डाले। इस्लाम ने धर्म की उस संन्यासयुक्त अवधारणा का निषेध किया है कि किसी व्यक्ति को कठोरतम तपस्याओं और जानलेवा साधनाओं से गुज़रे बिना पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि अगर दो कामों में एक का विकल्प नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने प्रस्तुत किया जाता तो उस काम को करते जिसे सरलतापूर्वक किया जा सकता या अधिक आसान होता। फिर आप अपनी उम्मत की आसानी को भी दृष्टि में रखते थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कार्यनीति उम्मत के लिए एक आदर्श है।
जिस प्रकार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मानव जाति में सबसे बढ़कर दानशील थे, जैसा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है कि “मैं मानवों में सबसे बढ़कर दानशील हूँ" (बैहक़ी), ठीक उसी प्रकार सारे इनसानों में सबसे बढ़कर गुनाहों से दूर रहनेवाले भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) थे। एक नबी की वास्तव में यही छवि होती है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सच्चा अनुसरण वास्तव में यही होगा कि हम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इन दोनों ही विशेषताओं को ग्रहण करने का प्रयास करें।
व्यर्थ बातों से बचना
(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश-स्मरण में अधिक लगे रहते थे। व्यर्थ बातें बहुत कम करते। नमाज़ को सुदीर्घ और भाषण को संक्षिप्त करते। आप विधवा और निर्धन के साथ चलने में लज्जा महसूस न करते और उनका हर काम कर देते थे। (हदीस : नसई, दारमी)
व्याख्या : आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अधिकाधिक ईश्वर को याद करते। प्रत्येक वह चीज़ जो ईश्वर की याद से सम्बन्धित हो, ईश-स्मरण में सम्मिलित है। आप विभिन्न तरीक़ों से प्रत्येक क्षण अल्लाह को याद किया करते।
वास्तविक जीवन ईश्वर की याद और उसके स्मरण से सम्बन्ध रखता है। जिस जीवन में ईश्वर का स्मरण न हो वह जीवन नहीं, वह सन्ताप और अभावग्रस्तता है। यह अलग बात है कि कोई व्यक्ति इस बात को महसूस न कर रहा हो।
दुनिया की बातों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कम ही रुचि लेते। सांसारिक बातें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बहुत कम करते थे। यूँ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सांसारिक बातें भी हिक्मत और मस्लहत से रहित न होती थीं। वास्तविक अर्थों में उन्हें व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उपलक्ष्य स्वरूप उन्हें व्यर्थ कहा गया है। व्यर्थ बातों से अभिप्रेत ऐसी निरर्थक बातें होती हैं जिनका कोई वास्तविक उद्देश्य न हो और जो ईश्वर की याद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध न रखती हों। स्पष्ट है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से ऐसी व्यर्थ बात निकल ही नहीं सकती थी।
मूल में थोड़े के लिए 'क़लील' शब्द प्रयुक्त हुआ है। क़लील सर्वथा निषेध के अर्थ में भी आता है। इस लिहाज़ से कुछ लोगों ने इस हदीस का अर्थ यह बताया है कि अल्लाह के रसूल कभी मुख से व्यर्थ बातें निकालते ही न थे।
ईश्वर से विशिष्ट सम्बन्ध हो तो नमाज़ स्वाभाविक रूप से दीर्घ हो जाएगी। और अगर भाषण में अनावश्यक बातों से बचा जाए, केवल आवश्यक और काम की बातें करने को पर्याप्त समझा जाए तो भाषण कभी लम्बा और उकता देनेवाला नहीं हो सकता। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा है—
“आदमी की लम्बी नमाज़ और उसका संक्षिप्त भाषण उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।" (हदीस : मुस्लिम)
यह आदमी की नादानी और नासमझी की बात होगी कि वह भाषण तो बहुत लम्बा दे लेकिन नमाज़ जो मूलतः अभीष्ट है, उसे संक्षिप्त कर दे।
नबी के अन्दर किंचितमात्र भी अहंकार नहीं पाया जाता था। हालाँकि ईश्वर ने उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया था।
सत्यवादिता और खरापन
(1) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अबू-जहल ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि (ऐ मुहम्मद) हम (क़ुरैश के लोग) तुम्हें नहीं झुठलाते। हम तो उस चीज़ को झुठलाते हैं जो तुम लेकर आए हो। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : अर्थात हमपर तुम्हारा सत्य प्रकाशमान और दिन की भाँति स्पष्ट है। हमने कभी भी तुम को झूठ बोलते नहीं देखा। लोगों में सत्यवादिता और अमानत की दृष्टि से तुम जाने जाते हो। हम वास्तव में तुम्हारी किताब और शरीअत को मानना नहीं चाहते। हम उस वह्य को नहीं स्वीकार करते जिसे तुम प्रस्तुत कर रहे हो।
काश! सत्य का यह शत्रु समझ सकता कि जो व्यक्ति सांसारिक मामलों में लोगों से झूठ नहीं बोल सकता वह धर्म के मामले में झूठ कैसे बोलेगा! जिस व्यक्ति की स्पष्ट विशेषता सत्यवादिता है वह ईश्वर से सम्बद्ध कर के कोई ग़लत बात कैसे कहेगा!
वास्तव में मक्का के क़ुरैश के बड़े-बड़े सरदार ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और पूर्वाग्रह से ग्रसित थे जिसके कारण सत्य को स्वीकार करना उनके लिए सहज नहीं रह गया था।
लज्जा
(1) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर्दे में रहने वाली कुँवारी लड़कियों से भी अधिक लज्जाशील थे। जब कोई ऐसी बात देखते जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अप्रिय होती तो हम यह बात उनके चेहरे से मालूम कर लेते थे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात कोई अप्रिय और स्वभाव के प्रतिकूल बात देखते तो लज्जा के कारण यद्यपि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुख से कुछ न कहते लेकिन उस नागवारी के चिन्ह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख पर स्पष्ट दीख पड़ते थे।
पर्दे में रहनेवाली लड़कियाँ ज़्यादा शर्मीली और लज्जाशील होती हैं, किन्तु आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में हया और शर्म उनसे भी बढ़कर थी।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के स्वभाव में अश्लीलता न थी और न आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कोई अश्लील बात करते थे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
दानशीलता
(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों में सबसे अधिक दानशील थे और रमज़ान में अन्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक दानशील हो जाते थे। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : रमज़ान वास्तव में महीना ही नेकी का है। इसलिए इस महीने में दानशीलता में वृद्धि एक स्वाभाविक बात है।
सहीह बुख़ारी की एक हदीस से मालूम होता है कि जिब्रील (अलैहिस्सलाम) रमज़ान की प्रत्येक रात में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिलते थे और फिर आपके साथ क़ुरआन पढ़ते। जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से मिलते तो फ़ायदा पहुँचाने में तेज़ हवा से भी बढ़कर दानशील होते थे।
(2) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कोई चीज़ माँगी गई हो और जवाब में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 'नहीं' कहा हो। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात किसी माँगनेवाले को 'नहीं' कहकर वापस नहीं किया। प्रत्येक माँगनेवाले को कुछ न कुछ दिया। अगर अपने पास से कुछ देने को न हुआ तो क़र्ज़ लेकर दिया।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अगर मेरे पास उहुद पर्वत के बराबर भी सोना हो तो मेरी प्रसन्नता की चीज़ यही होगी कि मुझ पर तीन रातें भी न बीतें कि मेरे पास उसमें से कुछ शेष हो सिवाय इसके कि किसी ऋण को चुकाने के लिए मैं उसमें से कुछ रोक लूँ।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि दानशीलता नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चरित्र की अत्यन्त उभरी हुई विशिष्टता थी। धन जमा करने में नहीं बल्कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को धन को वितरित करने में प्रसन्नता होती थी। धन चाहे कितना ही अधिक हो उसके समाप्त होने पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दुखी होने के बजाए आनन्दित होते थे।
(4) हजरत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बकरियाँ माँगी जो दो पहाड़ों के बीच थीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वे सब उसे दे दीं। वह व्यक्ति अपनी क़ौम के पास आया और कहने लगा कि ऐ लोगो, मुसलमान हो जाओ, ईश्वर की सौगन्ध मुहम्मद इतना कुछ देते हैं कि दरिद्रता का भय नहीं रहता। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने न केवल यह कि माँगनेवाले को टाला नहीं बल्कि देने में अत्यन्त दानशीलता का परिचय दिया।
हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक व्यक्ति मात्र दुनिया के लिए मुसलमान होता लेकिन फिर इस्लाम उसकी दृष्टि में सारी दुनिया से बढ़कर प्रिय हो जाता। यह था सत्यधर्म का चमत्कार और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की संगति का प्रभाव कि दुनिया चाहनेवाला भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निकट आकर सत्यवान बन जाता था।
(5) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तुम जानते हो कि सबसे बढ़कर दानशील कौन है?" सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आपने कहा, "सबसे बढ़कर दानशील अल्लाह है। फिर आदम की सन्तान में सबसे अधिक दानशील मैं हूँ और मेरे बाद इनसानों में से सबसे बढ़कर दानशील वह है जो ज्ञान प्राप्त करके उसको फैलाए। ऐसा व्यक्ति क़ियामत के दिन एक अमीर के रूप में आएगा या फिर वह इस तरह आएगा कि उसे अपने आप में एक समुदाय की हैसियत प्राप्त होगी।" (हदीस : अल-बैहक़ी)
व्याख्या : दानशीलता वास्तव में जीवन का प्रतीक है। जहाँ जितना जीवन पाया जाएगा वहाँ उतनी ही दानशीलता भी पाई जाएगी। ईश्वर चूंकि सर्वथा जीवन और जीवन का स्रोत है इसलिए उससे बढ़कर किसी दानशील की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आकाश और धरती ईश्वर की दानशीलता और उसके अनुग्रह और अनुकम्पा का जीवित प्रमाण हैं। ईश्वर के बाद दानशीलता के गुण से सर्वाधिक आभूषित उसके नबी होते हैं। इसलिए कि ईश्वरीय गुणों की प्रतिछाया उनके जीवन में सबसे अधिक परिलक्षित होती है।
फिर दानशीलता का सम्बन्ध मात्र धन ही से नहीं होता। सबसे बढ़कर दानशीलता और उपकार की बात यह है कि दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का प्रयास किया जाए। यही कारण है कि इस हदीस में आदम की सन्तान में सबसे बढ़कर दानशील उस व्यक्ति को घोषित किया गया है जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि से सुसज्जित होकर दुनिया में ज्ञान के प्रकाश को फैलाए ताकि लोग पथभ्रष्टता के अन्धकार से मुक्त हो सकें। उनके लिए वास्तविक आनन्द की सामग्री उपलब्ध हो सके और उन्हें दुनिया और आख़िरत में वास्तविक सफलता और कल्याण प्राप्त हो सके।
करुणा
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"कोई भी मोमिन ऐसा नहीं जिसका मैं दुनिया और आख़िरत में सर्वाधिक प्रिय न हूँ। अगर चाहो तो पढ़ लो कि नबी ईमानवालों से स्वयं उनकी अपनी जानों से भी अधिक निकट है।" (33:6)
अतएव जिस मोमिन को मृत्यु आए और वह माल छोड़े तो उसके ‘असबह' उसके वारिस होंगे, जो भी मौजूद हों। और जो कोई कर्ज़ छोड़े या छोटे बाल-बच्चे, वह मेरे पास आए मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात अगर उसने अपने पीछे धन-सम्पत्ति छोड़ी है तो यह उसके वास्तविक उत्तराधिकारियों को मिलेगी लेकिन कोई अपने पीछे ॠण या ऐसे बच्चे आदि छोड़ रहा है जिनके भरण-पोषण के बारे में वह चिन्तित है तो उसे परेशान और चिन्ताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का आत्मीय और स्वजन मैं हूँ। उसका ऋण चुकाना मेरा दायित्व होगा और उसके बच्चों के लालन-पालन की ज़िम्मेदारी मेरी होगी।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस्लामी राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से यह बात कही। इससे भली-भान्ति अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सरकार के दायित्त्व कितने विस्तृत और महत्वपूर्ण होते हैं और इस्लामी राज्य की मनोवृत्ति क्या होती है।
(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सुनने और आज्ञापालन पर बैअ्त करते थे तो आप कहते थे कि—
“यह भी कहो कि जितना मुझसे हो सकेगा।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हदीस के रावी का वर्णन है कि जब हम लोग इस बात पर बैअ्त करते कि हम हुक्म सुनेंगे और उसे मानेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह कहते कि अपने वचन में इन शब्दों को और जोड़ लो कि हम आज्ञापालन अपनी सामर्थ्य भर करेंगे। यह वास्तव में आप की करुणा थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते थे कि अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो तो वह उसके लिए ईश्वर के यहाँ गुनाहगार न ठहरे।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"ऐ अल्लाह मैं एक मनुष्य हूँ। अतएव जिस किसी मुस्लिम व्यक्ति को बुरा कहूँ या लानत करूँ या मारूँ तो इसे उसके लिए उत्कृष्टता और दयालुता बना दे।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मैं एक मनुष्य हूँ अर्थात मनुष्य होने के नाते कमज़ोरियाँ मुझमें भी हो सकती हैं। सम्भव है कि क्रोध की अवस्था में किसी मुसलमान को बुरा भला कहूँ, उसे लानत-मलामत करूँ या उसे मारूँ तो प्रभुवर, तू इसे उस व्यक्ति के लिए अपनी दया और अनुग्रह का निमित्त बना दे। मेरी बददुआ उस व्यक्ति के लिए दुआ बन जाए। एक हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ अल्लाह, जिस किसी मोमिन को मैंने बुरा-भला कहा हो तो इसको क़ियामत के दिन उसके लिए अपने सामीप्य का साधन बना दे।” (हदीस : बुख़ारी)
दयालुता
(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निवेदन किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, (अपने शत्रु) बहुदेववादियों को शापित करें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मुझे वास्तव में लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि मुझे तो रहमत (सर्वथा दयालुता) बनाकर भेजा गया है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात मेरा प्रमुख गुण रहमत है। यह चीज़ मुझे शोभा नहीं देती कि मैं शापित करूँ यद्यपि बहुदेववादी मेरी शत्रुता में अत्यन्त सक्रिय हैं। मुझे भेजे जाने का प्रयोजन तो यह है कि मैं लोगों को ईश्वरीय अनुकम्पा से निकट करने के लिए प्रयासरत रहूँ। इस स्थिति में यह चीज़ मुझे कदापि शोभा नहीं देती कि लानत और बद्दुआ करने में मेरी रुचि हो।
संवेदना
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ अबू-सैफ़ लोहार के यहाँ गए जो [नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेटे] इबराहीम की दूध-पिलाई माँ के पति थे। अल्लाह के रसूल ने इबराहीम को गोद में लेकर उनका चुम्बन लिया और उन्हें सूँघा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हम फिर अबू-सैफ़ के यहाँ गए। इबराहीम उस समय मरणासन्न दशा में थे। यह देखकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखों में आँसू आ गए। अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी रोते हैं! आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ऐ इब्ने-औफ़! यह रहमत है।" इसके बाद फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखों से आँसू जारी हो गए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “आँखें रो रही हैं और हृदय दुखी है मगर हम इसके बावजूद मुख से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ऐ इबराहीम, निश्चय ही हम तेरी जुदाई से शोकाकुल हैं।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : बेटे (इबराहीम) को सूँघा अर्थात बेटे को प्यार किया। मुँह के साथ नाक उनके मुँह पर इस प्रकार रखी जैसे कोई फूल सूँघता हो। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बेटे हज़रत इबराहीम अभी सोलह-सत्रह महीने ही के थे कि उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ उनकी बीमारी और मरणासन्न अवस्था का उल्लेख किया गया है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जब यह देखा कि कलेजे का टुकड़ा सदैव के लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से विलग होने को है तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखों से आँसू जारी हो गए।
हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के यह कहने का कि “ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी रोते हैं” अर्थ यह है कि ऐसे दुखद अवसर पर तो साधारण लोग रोते ही हैं, किन्तु हम समझते थे कि यह बात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की महानता के प्रतिकूल है कि आप भी आँसू बहाएँ।
"ऐ इब्ने-औफ़, यह रहमत है" यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का उत्तर था। अर्थात दयाभाव और प्रेम तो यही है कि ऐसे अवसरों पर आदमी को दुख हो और उसकी आँखें नम हो जाएँ। यह महानता के प्रतिकूल कदापि नहीं है। पैग़म्बर दुनिया में इसलिए नहीं आता कि वह लोगों को भावशून्य और संवेदनहीन बना दे बल्कि वह उनको जीवन का सही और स्वाभाविक मार्ग दिखाने आता है। मानव जीवन में सुख और दुख के अवसर आते ही रहते हैं। दुख के अवसर पर आदमी दुख प्रकट करे लेकिन उसे ईश्वर के फ़ैसले पर कोई शिकायत न हो। मानव के लिए सर्वाधिक उत्तम और सही नीति यही है।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने नवासे के निधन पर भी अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) के यहाँ गए थे। जाने से पहले आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहला भेजा था कि—
"वह चीज़ ईश्वर ही की है जो उसने ले ली और वह भी उसी की है जो उसने दे रखी हो। अतएव तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और प्रतिदान का इच्छुक होना चाहिए।" बेटी के आग्रह पर जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनके यहाँ गए और बच्चे को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की गोद में दे दिया गया तो उस समय वह मरणासन्न अवस्था में था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आँखें भीग गईं। हज़रत साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, यह क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यह रहमत है जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के दिलों में रखा है। अतः अल्लाह अपने बन्दों में से केवल उन्हीं लोंगों पर रहमत करता है जिनके दिलों में दयाभाव पाया जाता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
अर्थात यह दयाभाव है, जो प्रशंसनीय है, अप्रशंसनीय नहीं। ऐसे अवसरों पर जो चीज़ अवैध है वह कपड़े फाड़ लेना और मातम के साथ रोना आदि है।
दुख और सदमे का आदमी पर जो स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है उसको हेय समझना संकुचित दृष्टिकोण और धर्म के मूल स्वभाव से अनभिज्ञ होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
ख़ुशमिज़ाजी
(1) हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि जब से मैं मुसलमान हुआ, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझे अन्दर आने से कभी नहीं रोका, और जब भी मुझे आप ने देखा, हँसे। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात कभी भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझसे शुष्कता से नहीं मिले बल्कि हमेशा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रसन्न मुद्रा में मिले।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक दिन सहाबा ने कहा—
“ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमसे विनोद करते हैं?"
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं (हास्य में भी) सच्ची बात ही कहता हूँ।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : सहाबा का यह कहना कि “ऐ अल्लाह के रसूल आप हम लोगों से विनोद करते हैं" सहाबा को सम्भावतः यह ख़याल हुआ कि शायद यह चीज़ पैग़म्बर के प्रतिष्ठानुकूल न हो। क्योंकि रुतबे और स्थान की दृष्टि से वे अत्यन्त उच्च होते हैं।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन कि 'मैं सच्ची बात ही कहता हूँ' का अर्थ है कि मैं हास्य और विनोद में भी मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखता हूँ। उदाहरणार्थ मेरे हास्य में कोई झूठी और लचर बात कदापि नहीं होती।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक बूढ़ी औरत से कहा—
(जब उसने आप से कहा कि मेरे लिए आप दुआ करें कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूँ), “बूढ़ी औरत स्वर्ग में न जाएगी।" उसने कहा कि आख़िर उन्होंने क्या क़ुसूर किया है? वह औरत क़ुरआन पढ़ी हुई थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "क्या तुमने क़ुरआन में यह नहीं पढ़ा है—
“निश्चय ही हमने उन औरतों को (स्वर्ग में) एक विशेष उठान पर उठाया और हमने उन्हें कुँवारियाँ बनाया।" (56:35-36) (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : इस हदीस से ज्ञात होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शुष्क मिज़ाज नहीं थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने सहाबा के साथ विनोदपूर्ण बातें भी करते थे। लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की विनोदपूर्ण बातों में सूक्ष्म हास्य होता था। सन्तुलित हास्य वस्तुतः चित्त की स्वस्थता का प्रमाण है। शर्त यह है कि इसका उद्देश्य किसी का दिल तोड़ना या कष्ट देना न हो और यह भी आवश्यक है कि आदमी हर समय हँसी-मज़ाक़ ही न करता रहे क्योंकि इससे उसकी गरिमा और व्यक्तित्व को बड़ा आघात पहुँचता है।
(4) हज़रत अदी-बिन-हातिम (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि जब आयत, “(खाओ-पियो) यहाँ तक कि तुम्हें फ़ज्र की सफ़ेद धारी (रात्रि की) स्याह धारी से भिन्न नज़र आने लगे” अवतरित हुई तो अदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने तकिये के नीचे दो डोरियाँ, एक सफ़ैद और एक स्याह रंग की, रखता हूँ। इसी से मैं रात को दिन से अलग पहचान लेता हूँ। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम्हारा तकिया तो बड़ा लम्बा-चौड़ा है! अरे यह तो संकेत है। रात के अन्धेरे और दिन के उजाले की ओर।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : हज़रत अदी-बिन-हातिम (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ग़लती से क़ुरआन की आयत में उपलक्ष्य का शाब्दिक अर्थ ले लिया और दो डोरियाँ एक काली और एक सफ़ेद रंग की अपने तकिए के नीचे रखकर सोने लगे। और जब इतना उजाला हो जाता कि वे डोरियों को देखकर यह पहचान लेते कि यह सफ़ैद डोरी है और यह काली तो खाना-पीना बन्द कर देते।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से विनोदपूर्वक यह कहा कि तुम्हारा तकिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है कि प्रातः बेला उसके नीचे उदित होती है। फिर आप ने स्पष्ट कर दिया कि सफ़ैद और स्याह धागे से अभिप्राय वह नहीं है जो तुमने समझा है बल्कि इससे रात का अँधेरा और दिन की सफ़ैदी अभिप्रेत है जो क्षितिज में प्रकट होती है। उसका तुम्हारे तकिये के नीचे रखी हुई स्याह और सफ़ेद डोरी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
दिल रखना
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब किसी व्यक्ति से मुसाफ़ह करते (हाथ मिलाते) तो अपना हाथ उस समय तक अलग न करते जब तक कि वह व्यक्ति अपना हाथ अलग न कर लेता। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस समय तक उसकी ओर से मुँह न फेरते जब तक कि वह व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने से अपना मुँह न हटा लेता। इसके अतिरिक्त आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कभी किसी ने इस हाल में नहीं देखा कि आप अपने घुटने अपने साथ बैठनेवाले के सामने करके बैठे हों। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुशीलता और प्रेमभाव का हाल यह था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किसी से मुसाफ़ह करते तो जब तक दूसरा व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हाथ न छोड़ता आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपना हाथ उसके हाथ से अलग न करते। और जब तक वह व्यक्ति स्वयं आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने से न हट जाता आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसकी ओर से अपना चेहरा न हटाते, बल्कि उसकी ओर उन्मुख रहते।
मजलिस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने को लोगों से श्रेष्ठतर और बड़ा सिद्ध करने के लिए कोई विशिष्ट तौर-तरीक़ा न अपनाते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब सबके साथ बैठते तो अपना घुटना आगे बढ़ाकर न बैठते। हदीस के कुछ टीकाकारों की दृष्टि में इससे अभिप्रेत यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों के सामने घुटने खड़े करके न बैठते और कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ यह लिया है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कभी किसी के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठा करते थे।
(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि (एक बार) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमारी एक सेना भेजी। लोग दुश्मन के मुक़ाबले से भाग खड़े हुए। मदीना वापस आए तो (पश्चाताप और लज्जा के कारण) छिप रहे। और हमने कहा कि सर्वनाश हुआ हमारा! फिर हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), हम तो फ़रार होनेवाले लोग हैं। नबी ने कहा—
“नहीं, बल्कि तुम हमले पर हमला करनेवाले लोग हो, और मैं तुम्हारी जमाअत हूँ।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : "सर्वनाश हुआ हमारा" अर्थात हमने अक्षम्य अपराध किया है। इसलिए अब हमें हलाकत और तबाही से कोई नहीं बचा सकता।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने डाँटने के बजाय प्रेमपूर्वक अपने साथियों का उत्साहवर्द्धन किया और उनका दिल रखने के लिए कहा कि बात यह नहीं है कि तुम लोग जिहाद के मैदान से फ़रार हुए हो बल्कि तुम तो पलट-पलटकर लड़नेवाले लोग हो। भागनेवाले दूसरे हुआ करते हैं। यूँ भी युद्ध की चालों के तहत किसी लश्कर का पीछे हटना और ताज़ा कुमक के साथ दोबारा मैदान में उतरने की फ़िक्र करना कोई जुर्म भी नहीं है।
“और मैं तुम्हारी जमाअत हूँ” अर्थात मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे अलग नहीं हूँ। तुमको इस सामयिक पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पीछे अल्लाह के रसूल की शक्ति है। और अल्लाह का रसूल अपने आप में पूरी एक जमाअत की हैसियत रखता है। तुम तनिक भी दिल छोटा न करो। ईश्वर की सहायता और मदद तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी।
(3)
गरिमा और महानता
सुदृढ़ता
(1) हज़रत अल-क़मा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है, वे कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से पूछा। वे कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल के कर्म का क्या हाल था? क्या किसी इबादत के लिए आप किसी दिन को विशिष्ट करते थे? कहा, "नहीं, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कर्म सदैव के लिए था। और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सुदृढ़ता प्राप्त थी।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो कर्म भी अपनाते और जो उपासना भी करते उसे नियमित रूप से करते थे। उसे त्याग देना आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को स्वीकार न होता। यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चरित्र की विशिष्टता थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा गया कि कौन-सा कर्म ईश्वर को बहुत पसन्द है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “जिसकी पाबन्दी हमेशा की जाए चाहे वह थोड़ा ही हो।”
वे कर्म ही आदमी के चरित्र और व्यक्तित्व का वास्तविक अंग होते हैं जिन्हें वह संकल्प और दृढ़ता के साथ अपनाता है और कभी उन्हें त्यागने का इरादा नहीं करता।
क्षमाशीलता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने दो कर्मों में से एक के करने का विकल्प होता तो आप उनमें से जो आसान होता उसी को अपनाते। शर्त यह है कि उस कार्य के गुनाह होने की सम्भावना न होती, और अगर उसके गुनाह होने की सम्भावना होती तो आप सबसे अधिक उससे दूर रहनेवाले व्यक्ति थे। और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी किसी बात में अपने लिए किसी से भी प्रतिशोध नहीं लिया। अलबत्ता ईश्वरीय प्रतिष्ठा की अवहेलना पर आप अवश्य अल्लाह के लिए उसका दण्ड देते थे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) स्वयं अपने लिए कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते थे। शरीअत की मार्यादाओं और उसके आदेशों की अवहेलना करनेवालों को यदि दण्ड दिए गए तो वे दण्ड ईश्वरीय आदेश के तहत दिए गए हैं। उनके पीछे कोई प्रतिशोध-भावना कार्यरत नहीं रही है। दण्ड उन्हीं को मिला जो ईश्वर की ओर से दण्ड के भागी हो चुके थे।
(2) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न औरत को और न सेवक को, न किसी और को, सिवाय इस परिस्थिति के जबकि आप ईश्वरीय मार्ग में जिहाद कर रहे होते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कोई व्यक्तिगत कष्ट और पीड़ा पहुँची हो और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कष्ट देनेवाले से बदला लिया हो। अलबत्ता अगर ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन होता तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ईश्वर के लिए अवश्य उसपर दण्ड देते। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : मालूम हुआ कि क्षमा और दरगुज़र से काम लेना आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वभाव था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते थे चाहे वह बीवी हो या सेवक या कोई और। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सदैव लोगों की ग़लतियाँ क्षमा कर दिया करते थे और बदला लेने से हमेशा बचते थे। विशालहृदयता के बिना नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस तरीक़े पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है।
क्षमा और दरगुज़र से काम लेना और लोगों की ग़लतियों और उनके क़ुसूरों को माफ़ कर देना कदाचित् उच्चतम कोटि की दानशीलता है।
सहनशीलता
(1) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ चल रहा था। उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जिस्म पर नजरान की बनी हुई मोटे किनारे की चादर थी। एक आराबी (ग्रामीण) आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मिला। उसने आप को अत्यन्त कठोरतापूर्वक, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की चादर पकड़ कर खींचा। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उसके ज़ोर से खींचने के कारण नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की गर्दन पर चादर के किनारे का निशान पड़ गया। फिर उसने कहा कि मुझे भी अल्लाह के उस माल में से, जो तुम्हारे पास है, कुछ देने का आदेश दो। इसपर आप उसकी ओर उन्मुख हुए और हँसे और उसे कुछ देने का आदेश दिया। (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यह घटना हुनैन के युद्ध से वापसी के समय की है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस ग्रामीण की धृष्टता पर कुछ ध्यान न दिया बल्कि हँसकर टाल दिया और उसकी माँग भी पूरी कर दी।
(2) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक व्यक्ति बैठा था जिसपर (कुसुम या केसर से रंगा हुआ) पीले रंग का कपड़ा था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वभाव यह था कि आप अप्रिय बात को रू-बरू मना न करते थे (इसलिए मौन रहे) फिर जब वह व्यक्ति चला गया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा—
“तुम लोग उसको पीले कपड़े से मना कर देते तो अच्छा होता।" (हदीस : इमाम तिरमिज़ी की शमाएल)
व्याख्या : यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नितान्त सौम्यता और करुणा थी कि अधिकतर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) रू-बरू ऐसे कार्यों से मना न करते कि आदमी लज्जित हो या उसकी ओर से कोई बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त हो। लेकिन अगर इस तरह का भय न होता तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तत्काल ही त्यागने योग्य चीज़ों को त्याग देने का निर्देश देते।
यहाँ यह बात भी दृष्टि में रहे कि मुँह पर टोकने और किसी बात से मना करने में आप उस समय जल्दी नहीं करते थे जबकि वह बात मात्र उत्तमता के विरुद्ध होती या उसके त्यागने में विलम्ब होने से कोई बड़ी हानि न होती। अन्यथा जो कार्य स्पष्टतः अवैध होता उसके करने और सत्य का उल्लंघन करने की स्थिति में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नीति कदापि यह न होती थी।
(3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना आए तो अबू तलहा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास ले गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अनस होशियार लड़का है। यह आप की सेवा में रहेगा। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का कथन है कि फिर मैंने यात्रा-अन्यात्रा हर हाल में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा की। ईश्वर की सौगन्ध, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किसी काम को जो मैंने किया यह नहीं कहा कि—
“तूने ऐसा क्यों किया।" और जिसको मैंने नहीं किया उसके विषय में यह नहीं कहा कि “तूने ऐसा क्यों नहीं किया।” (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : यह असाधारण गुण उसी व्यक्तित्व में पाया जा सकता है जो ईश्वर के बन्दों पर अत्यन्त मेहरबान और अपने सेवकों के लिए अत्यन्त दयालु हो और जिसको ईश्वर की ओर से असाधारण धैर्य और मानसिक शान्ति (Peace Of Mind) की निधि प्राप्त हो।
अल्लाह पर भरोसा
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने लिए कोई चीज़ कल के लिए जमा करके न रखते थे। (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मतलब यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ईश्वर पर इतना पूर्ण विश्वास और उसके दया-भण्डार पर ऐसा भरोसा था कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने लिए किसी चीज़ को संजोकर रखने का प्रयास नहीं करते थे कि वह कल काम आएगी। यह नीति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) केवल अपने साथ अपनाते थे अन्यथा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने घरवालों के लिए साल भर का ख़र्च जमा करके रख देते थे कि सम्भव है कि ज़रूरत के समय वे अधीर हो जाएँ और उन्हें परेशानी हो।
(2) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि वे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ उस युद्ध में सम्मिलित थे जो नज्द के निकट हुआ था। फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिहाद से वापस हुए तो जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ वापस हुए। सहाबा दोपहर में एक ऐसी घाटी में पहुँचे जिसमें कीकर के वृक्ष भारी संख्या में थे। अल्लाह के रसूल (सहाबा के साथ) वहीं उतरे और तमाम लोग छाया ढूँढते हुए इधर-उधर के वृक्षों के नीचे जा पड़े। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी कीकर के एक वृक्ष के नीचे ठहरे और अपनी तलवार उस वृक्ष पर लटका दी। (हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि) हम लोग थोड़ी नींद लेने के लिए गए कि अचानक हमने सुना कि अल्लाह के रसूल हमें आवाज़ दे रहे हैं। (हम लोग वहाँ पहुँचे तो) क्या देखते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक देहाती मौजूद है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इसने मुझ पर मेरी तलवार खींची जबकि मैं सो रहा था। और जब मेरी आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरी नंगी तलवार इसके हाथ में है। इसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैंने कहा कि अल्लाह। यह बात तीन बार कही।" और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस देहाती को कोई दण्ड नहीं दिया, और उठकर बैठ गए।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ऐसे नाज़ुक मौक़े पर भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तनिक भी घबराए नहीं और अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा और विश्वास व्यक्त किया।
एक अन्य रिवायत से मालूम होता है जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा तो उस देहाती के हाथ से तलवार गिर गई। और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे उठा लिया और कहा कि अब बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? उसने कहा कि आप तो भलाई के साथ पकड़ करनेवाले आदमी हैं। (अर्थात मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मुझे कृपापूर्वक क्षमा कर देंगे और मेरे विरुद्ध कोई बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे।) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।” (अर्थात जब तुझे मुझपर भरोसा है तो तुझे मेरे आमन्त्रण और मेरे सन्देश के सत्य होने पर विश्वास करना चाहिए।) उसने कहा कि नहीं अलबत्ता यह प्रण करता हूँ कि न मैं स्वयं आपसे लड़ूँगा और न आपसे लड़नेवालों का साथ दूँगा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे छोड़ दिया। वह अपने साथियों के पास गया और बोला, “मैं तुम्हारे पास एक सर्वोत्तम व्यक्ति के पास से होकर आ रहा हूँ।" (किताबे-हुमैदी, रियाज़ुस्सालिहीन, इमाम मुहियुद्दीन)
सौम्यता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अन्दर आने की अनुमति चाही। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“यह व्यक्ति अपने कुटुम्ब में अत्यन्त बुरा है।" (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आज्ञा दे दी) फिर जब वह अन्दर आया तो आप उससे खुलकर मिले और उससे बात की। जब वह चला गया तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब उस व्यक्ति ने अनुमति माँगी तो आप ने कहा कि यह व्यक्ति अपने कुटुम्ब में सबसे बुरा है, फिर जब वह अन्दर आया तो आप उससे खुलकर मिले। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "ऐ आइशा, अल्लाह दुष्भाषियों और दुर्वक्ता को पसन्द नहीं करता।" (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात बुरे लोगों के साथ भी हम सदव्यवहार ही करें, अल्लाह को यही चीज़ पसंद है। किसी कुचरित्र व्यक्ति के कारण हम सदाचार को कदापि न छोड़ें।
आदमी नैतिकता की दृष्टि से कैसा है, इसका अन्दाज़ा इससे भली-भाँति किया जा सकता है कि वह लोगों से कैसे मिलता है और लोगों से उसकी बात-चीत कैसी होती है। फिर नैतिक सौन्दर्य और विनम्रता का प्रभाव यह है कि इसके द्वारा बड़े से बड़ा शत्रु भी राम हो सकता है। इसलिए व्यवहार-नीति की अपेक्षा यही है कि हम हमेशा और हर हाल में सदाचार और सुशीलता को दृष्टि में रखें।
वीरता
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सब लोगों से अधिक सुन्दर, सर्वाधिक दानशील और सर्वाधिक वीर थे। एक बार रात को एक आवाज़ सुनकर मदीनावाले व्याकुल और भयभीत हो गए। उल्लेखकर्ता का बयान है कि फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्हें मिले। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अबू-तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घोड़े पर, जिसपर ज़ीन न थी, सवार थे और तलवार आप की गर्दन में लटकी हुई थी। आप ने कहा, “डरो नहीं, डरो नहीं।” फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “मैंने इस घोड़े को दरिया के सदृश वेगवान और तीव्रगामी पाया।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : एक रात मदीना के लोगों को किसी ओर से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि मदीनावालों को चोरों या दुश्मनों का भय हुआ। लोगों ने जिधर से आवाज़ सुनी थी, उस ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सबसे पहले बिल्कुल अकेले दुश्मन की ख़बर लेने घर से निकल पड़े थे और यह पता लगाकर वापस लौट रहे थे कि दुश्मन आदि की शंका सही नहीं थी। वस्तुस्थिति मालूम करने के लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पहल करना और अकेले घर से निकल पड़ना बड़े साहस और वीरता की बात थी।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने लोगों को इतमीनान दिलाया कि कोई ख़तरा नहीं है इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं।
इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर ख़तरे की कोई आहट मिले तो वस्तुस्थिति की जाँच के लिए अकेले निकल पड़ना अच्छी बात है। शर्त यह है कि जान का यक़ीनी ख़तरा न हो। लेकिन ऐसे अवसर पर ख़ाली हाथ बिना हथियार के निकलना ठीक नहीं।
(2) हज़रत बरा-बिन-आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि ख़ुदा की क़सम! जब कभी रक्तिम और घमसान का युद्ध होता तो हम लोग नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आड़ में अपना बचाव करते थे। और निश्चय ही वीर हममें वे थे जो लड़ाई का सामना करते अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अर्थात ऐसे नाज़ुक अवसर पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आगे होते और हम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपनी ओट बना लेते। इससे भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वीरता और साहस का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। जिसका अल्लाह पर ईमान होता है और जो ईश्वरीय सहायता पर विश्वास रखता है वह कभी मृत्यु को महत्व नहीं देता। मृत्यु भी ऐसे व्यक्ति के लिए अमर जीवन का एक सन्देश होती है। अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बढ़कर ईमान और विश्वास किसको प्राप्त हो सकता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्नीस युद्धों में सम्मिलित हुए। आप मात्र एक आमन्त्रणदाता ही न थे बल्कि इस्लामी सेना के एक सर्वश्रेष्ठ सेनापति और ईश्वरीय मार्ग के एक जाँबाज़ मुजाहिद भी थे।
आत्मसम्मान
(1) हज़रत मुग़ीरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि सअ्द-बिन-उबादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि अगर मैं किसी परपुरुष को अपनी पत्नी के साथ देखूँ तो मैं उसे तलवार से मार दूँ और तलवार के पीछे की ओर से नहीं बल्कि उसकी धार की ओर से। उनकी यह बात अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहुँची तो आपने कहा—
"क्या तुम्हें साद की ग़ैरत पर आश्चर्य हो रहा है। ईश्वर की सौगन्ध मैं उनसे कहीं अधिक ग़ैरतमन्द हूँ और मुझसे भी बढ़कर ग़ैरतदार ईश्वर है। इसी कारण उसने खुले और छिपे समस्त अश्लील कार्यों को अवैध ठहराया है। और उज़्र ईश्वर से बढ़कर किसी अन्य को प्रिय नहीं। इसी लिए अल्लाह ने डरानेवालों और शुभ-सूचना देनेवालों (पैग़म्बरों) को भेजा। और अल्लाह से बढ़कर कोई प्रशंसा को पसन्द नहीं करता। इसी लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : इस हदीस से कई बातें मालूम हुईं। एक यह कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की ग़ैरत (आत्मसम्मान) यह पसन्द नहीं करती कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के अंकपाश में सुख भोग करे, उसी प्रकार अल्लाह की ग़ैरत को भी यह स्वीकार नहीं कि उसके बन्दे किसी भी प्रकार के अश्लील और बेग़ैरती के काम में लिप्त हों। इसी लिए उसने ऐसे समस्त कार्यों को अवैध ठहरा दिया है जो अश्लीलता और निर्लज्जता के कार्य हैं।
दूसरी बात इस हदीस से यह मालूम हुई कि ईश्वर ने दुनिया में रसूलों और नबियों को इसी लिए भेजा ताकि क़ियामत के दिन कोई व्यक्ति यह उज़्र पेश न कर सके कि मुझे तो ईश्वर का कोई सन्देश मिला ही नहीं अन्यथा मैं जीवन पर्यन्त ईश्वर का अवज्ञाकारी बनकर कदापि न रहता। ईश्वर ने नबियों और रसूलों को इसी लिए नियुक्त किया कि हुज्जत पूरी हो सके और लोग अपनी अवज्ञा को अपनी मजबूरी क़रार न दे सकें और उन्हें यह शिकायत करने का अवसर न मिले कि उन्हें सत्य का मार्गदर्शन करनेवाला कोई मिला ही नहीं। क़ुरआन में भी है—
रसूल शुभ सूचना देनेवाले और सचेत करने वाले बनाकर भेजे गए ताकि रसूलों के पश्चात लोगों के पास अल्लाह के मुक़ाबले में (अपने निर्दोष होने का) कोई तर्क न रहे। (4 : 165)
इमाम नव्वी के अनुसार उज़्र शब्द यहाँ 'इअज़ार' अर्थात उज़्र के दूर करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
तीसरी बात जो अल्लाह को प्रिय है और सबसे बढ़कर प्रिय है वह है सत्य को स्वीकार करना और गुणज्ञता का गुण। किसी की प्रशंसा वही कर सकता है जो पारखी हो। जहाँ मूल्यांकन (Appreciation) नहीं वहाँ संवेदनहीनता और अज्ञान के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं पाई जा सकती। ईश्वर स्वयं गुणज्ञ है इसी लिए उसने अपने प्रिय और वफ़ादार बन्दों की स्वयं प्रशंसा की है। अगर हम ईश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसको जानते और उसकी महानता से परिचित हैं। सत्य का इनकार करनेवालों के विषय में ईश्वर की टिप्पणी यह है कि—
"उन्होंने ईश्वर की क़द्र न पहचानी जैसी क़द्र पहचाननी चाहिए थी।" (6:92)
क़ुरआन की पहली ही आयत जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि (Finding) का पता देती है, "सब प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए ही हैं जो सारे संसार का प्रभु है।" (1:1)
सबसे बड़ा सत्य यही है। मानव जीवन में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति हो, सबसे सुन्दर बात यही हो सकती है। अगर किसी का जीवन वस्तुतः इस बड़े तथ्य को व्यक्त करने लगता है तो ईश्वर से बढ़कर कोई दूसरा उसका क़द्रदान नहीं हो सकता। वह अनिवार्यतः उसे विनष्ट होने से बचाएगा और अपनी जन्नत में उसे स्थान देगा।
विशालहृदयता
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
"हमारा कोई वारिस नहीं है। जो कुछ हमने छोड़ा वह सदक़ा है।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नैतिकता के इतने उच्च स्थान पर आसीन थे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए यह बात शोभनीय नहीं हो सकती कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जनसामान्य की तरह अपनी औलाद को अपने तर्के का वारिस बनाएँ। अल्लाह के नबी आत्मोत्सर्ग के जिस स्थान तक पहुँचे हुए होते हैं आम आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे वारिस एक दीनार भी बाँट नहीं सकते। मैं जो कुछ भी छोड़ जाऊँ उसमें से मेरी पत्नियों के ख़र्च और व्यवस्थापक के पारिश्रमिक के बाद जो बचे वह सद्क़ा है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : पत्नियों का ख़र्च और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक अर्थात इस मौलिक व्यय के बाद जो कुछ बचता है वह उत्तराधिकारियों में विभाजित नहीं हो सकता। वह उम्मत के ज़रूरतमन्दों के लिए ख़र्च किया जाएगा। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सन्तान आम लोगों की सन्तानों की भाँति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के तर्के में से अपने किसी हिस्से की माँग नहीं कर सकती। विरासत के रूप में वह एक दीनार भी नहीं बाँट सकती।
(3) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की धर्मपत्नी हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मृत्यु के बाद हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से अल्लाह के रसूल के उस तर्के में से अपना हिस्सा माँगा जो अल्लाह ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दिया था। हज़रत अबू-बक्र ने कहा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तो यह कहा है—
“हमारा कोई वारिस नहीं होता और हम जो कुछ छोड़ जाएँ वह सद्क़ा है।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : सहीह मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि हजरत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने ख़ैबर और फ़िदक और मदीने की आमदनी में से अपना हिस्सा माँगा था। हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने विवशता प्रकट की कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह कह गए हैं कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएँ उसकी हैसियत सदक़े की है। हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा—
“मैं किसी ऐसे कार्य को नहीं त्याग सकता जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) करते रहे हों। मैं डरता हूँ कि अगर मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के किसी कार्य को त्यागा तो पथभ्रष्ट हो जाऊँगा।" (हदीस : मुस्लिम)
इमाम नव्वी कहते हैं कि विद्वानों में यह मतैक्य पाया जाता है कि सारे ही नबियों का यही हाल है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता।
विनम्रता और विनयशीलता
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि—
“ऐ सृष्टजनों में सर्वश्रेष्ठ!" तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "वे तो इबराहीम थे।”
व्याख्या : कोई आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सृष्टजनों में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि से सम्बोधित करे, इसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी पसन्द नहीं किया। इसलिए कि यह विनयशीलता और विनम्रता के प्रतिकूल था। यह आपकी विनयशीलता थी कि आपने कहा कि "सृष्टजनों में सर्वश्रेष्ठ" की उपाधि के पात्र तो वास्तव में हज़रत इबराहीम (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं। फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के समक्ष हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की यह हैसियत भी थी कि वे ख़लीलुल्लाह (अल्लाह के प्रगाढ़ मित्र) और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पितामह थे। यूँ तो हदीसों से यह सिद्ध है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) समस्त नबियों के सरदार हैं लेकिन एक शिष्ट व्यक्ति चाहे वह कितनी ही प्रशंसा और प्रतिष्ठा का अधिकारी क्यों न हो, बहुधा वह अपनी तुलना में दूसरे ही को प्राथमिकता देता है।
(2) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुम मेरी प्रशंसा में सीमा से न बढ़ो जिस प्रकार ईसाई ईसा-बिन-मरयम की प्रशंसा में सीमा से आगे बढ़ गए हैं। मैं तो बस ईश्वर का बन्दा हूँ। अतः तुम मुझे ईश्वर का बन्दा और उसका रसूल कहो।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : ईसाई हज़रत ईसा मसीह (अलैहिस्सलाम) की प्रशंसा में सीमा से इतना आगे बढ़े कि उन्होंने हज़रत ईसा मसीह (अलैहिस्सलाम) को ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा बनाकर दम लिया। तुम्हें इस नीति से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनसान के लिए सर्वाधिक उच्च स्थान अगर कोई हो सकता है तो वह बन्दगी और दासत्व का स्थान है। दासत्व का गुण नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में अपनी पूर्णता को प्राप्त था। यही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की महानता का वास्तविक रहस्य है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की प्रशंसा में किसी ऐसी वर्णनशैली को अपनाने से बचना आवश्यक है जिससे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दासता का निषेध होता हो।
“मुझे ईश्वर का बन्दा और उसका रसूल कहो।” बन्दगी के गुण को रिसालत के साथ जोड़ने का प्रयोजन यह है कि यह एहसास सदैव जीवन्त रहे कि पैग़म्बर भी ईश्वर का बन्दा ही होता है किन्तु वह पूर्णत्व को प्राप्त बन्दा होता है। इस प्रकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुदेववाद की जड़ हमेशा के लिए काट दी।
(3) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि 'मदीनावालों की दासियों में से एक दासी थी। वह अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ती और जहाँ चाहती आप को ले जाती।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : अर्थात जब वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कुछ कहना-सुनना चाहती या उसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अपनी कोई परेशानी बयान करनी होती तो वह निस्संकोच जहाँ चाहती आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ले जाकर बातें कर लेती। इससे इस बात का भली-भाँति अन्दाज़ा किया जा सकता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में कितनी विनयशीलता और आत्मत्याग पाया जाता था। किसी दासी या लौंडी के साथ जाने और उसकी बातों को सुनने को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रतिकूल कदापि नहीं समझते थे। फिर इससे इस बात का भी पता चलता है कि अपनी उम्मत के एक-एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों न हो, आप कितने संवेदनशील थे और लोगों से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कितना हार्दिक लगाव रखते थे।
(4) हज़रत इब्ने-शिहाब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“किसी बन्दे के लिए यह उचित नहीं है कि वह यह कहे कि मैं (अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यूनुस-बिन-मत्ता से श्रेष्ठ हूँ।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इसे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विनयभाव और सौम्यता के प्रतिकूल समझा कि कोई नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को हज़रत यूनुस (अलैहिस्सलाम) से श्रेष्ठ कहे। यह बात दूसरे नबियों की प्रतिष्ठा और आदर के प्रतिकूल भी है। फिर यह संशय भी था कि कहीं लोग नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को श्रेष्ठ बतलाते हुए दूसरे नबियों को कमतर न समझने लगें।
(4)
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कैसे थे?
घरवालों के साथ
(1) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“तुममें सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो तुममें अपने घरवालों के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं अपने घरवालों के लिए तुम सबसे अच्छा हूँ।” (हदीस : तिर्मिज़ी, दारमी)
व्याख्या : आदमी का मामला सबसे पहले अपने घरवालों के साथ पेश आता है। इसलिए उसके अच्छे या बुरे होने की अभिव्यक्ति भी सबसे पहले घर ही पर होती है। इसलिए इस हदीस में किसी आदमी के अच्छे और बेहतर होने की पहचान यह बताई गई है कि तुम देखो कि उसका आचरण और व्यवहार अपने घरवालों, सगे-सम्बन्धियों और अपने अधीनस्थों के साथ कैसा है। अगर वह अपने घरवालों के लिए एक बेहतरीन व्यक्ति सिद्ध हो रहा है तो समझ लो कि वह वास्तव में एक बेहतरीन व्यक्ति है।
नबी चूँकि अपने समुदाय के लिए आदर्श होता है इसलिए जीवन के प्रत्येक मामले में उसे लोगों की तुलना में श्रेष्ठतम होना ही चाहिए।
(2) हज़रत असवद-बिन-यज़ीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से पूछा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने घर में होते थे तो क्या करते थे? उन्होंने कहा—
“नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने घरवालों के काम में लगे रहते थे और जब नमाज़ का समय आ जाता तो नमाज़ के लिए उठ खड़े होते।” (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : यानी घर में घर के लोगों की सेवा में लगे रहते, लेकिन नमाज़ का समय आते ही मसजिद के लिए चल पड़ते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जीवन में ईश्वर और उसके बन्दों दोनों ही के अधिकारों का पूरा ख़याल रखते थे। इस सिलसिले में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के यहाँ जो सन्तुलन पाया जाता है, वह अपनी मिसाल आप है।
(3) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी पत्नियों के मध्य मिलने की बारी और अन्य अधिकारों में पूरे तौर पर इनसाफ़ से काम लेते और दुआ करते—
“ऐ अल्लाह! मेरा यह न्यायपूर्ण बँटवारा तो वह है जो मेरे बस में है, मगर जिस चीज़ पर तुझी को अधिकार प्राप्त है, जो मेरे अधिकार से बाहर की चीज़ है अर्थात हृदय, (इसलिए यदि किसी पत्नी से मुझे विशेष हार्दिक लगाव है) तो इसपर तेरी ओर से मैं निन्दनीय न ठहरूँ।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने-माजा)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि अगर किसी के यहाँ एक से अधिक पत्नियाँ हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि पत्नियों के रोटी, कपड़े और दूसरी सभी ज़रूरी चीज़ों के मामले में इनसाफ़ से काम ले। किसी भी मामले में किसी पत्नी का हक़ न मारा जाए। अलबत्ता जहाँ तक हार्दिक झुकाव का सम्बन्ध है तो सम्भव है उसे अपनी किसी पत्नी से दूसरी पत्नियों की अपेक्षा अधिक प्रेम हो। इसपर ख़ुदा के यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि किसी का अपना दिल स्वयं उसके अपने बस में नहीं होता। अलबत्ता ईश्वर के यहाँ किसी प्रकार की पकड़ से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी व्यवहार और हक़ों के अदा करने में अपनी पत्नियों के मध्य सदैव न्याय से काम लेता हो।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अधिक किसी को भी अपने घरवालों पर मेहरबान नहीं देखा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सुपुत्र इबराहीम (जो मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा की कोख से थे), मदीना के ऊपरी क्षेत्र की ओर (एक दाई के यहाँ) दूध पीने के उद्देश्य से रखे गए थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) वहाँ उन्हें देखने के लिए जाया करते थे। हम भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ होते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) घर में प्रवेश करते थे, जहाँ धुआँ भरा होता था, इसलिए कि उनकी धाय के यहाँ लोहार का काम होता था। फिर बेटे को गोद में लेते, उन्हें प्यार करते और चुम्बन लेते, फिर लौटते। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : अरब की परम्परा के अनुसार बेटे इबराहीम को दूध पीने के लिए एक धाय (अन्ना) के सुपुर्द किया गया था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बेटे को देखने बराबर अबू-सैफ़ के यहाँ (जो हज़रत इबराहीम की धाय के पति थे) जाया करते थे। अबू-सैफ़ लोहार का काम करते थे। इसलिए उनके घर में धुआँ फैला रहता था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) धुएँ भरे घर में प्रवेश करने से न हिचकते। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) घर में प्रवेश करते और इबराहीम को देखते और प्यार करते, फिर वापस होते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपने बेटे इबराहीम से कितनी मुहब्बत थी इसका अन्दाज़ा इससे कर सकते हैं कि जब दुग्धपान की अवस्था में हज़रत इबराहीम की मृत्यु हुई तो हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“इबराहीम मेरा बेटा है और वह छाती के मध्य (अर्थात दूध पीने की अवस्था में) मरा है।" (हदीस : मुस्लिम)
(5) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मुझे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पत्नियों में से किसी के सिलसिले में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा का ऐसा प्रश्न पैदा नहीं होता था जैसा कि ख़दीजा के सिलसिले में पैदा होता था। मैंने ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को देखा नहीं था, लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनकी चर्चा हमेशा करते रहते। अकसर ऐसा होता कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बकरी ज़िब्ह करते, फिर उसके टुकड़े करते और ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की सहेलियों के यहाँ भेजते। मैं अधिकतर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहती कि मानो दुनिया में एक ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के सिवा कोई स्त्री थी ही नहीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते—
"यक़ीनन वह ऐसी और ऐसी (यानी बहुत अच्छी) स्त्री थीं और उनसे मुझे सन्तान हुई।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी चाहनेवाली पत्नी को उसकी मृत्यु के पश्चात भी भूल न सके, बल्कि बराबर याद करते रहते थे और उनकी सहेलियों के यहाँ उपहार भी भेजते रहते। यह दुनिया से जानेवाली पत्नी का एक हक़ था, जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अदा करते थे। और इस तरह अपनी जीवन संगिनी की याद को ताज़ा रखने का उपाय भी करते थे।
(6) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मेरी नज़र में आज भी यह दृश्य है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझे अपनी चादर की आड़ में ले लिया करते थे और मैं हब्शी लोगों को मसजिद में युद्ध-कला (और गद) का खेल खेलते देखती थी। जब तक कि मैं ख़ुद उससे उकता न जाती, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझे खेल दिखाते रहते। अतः लोगो, किशोरी की भावना का ख़याल रखो। उसे खेल और मनोरंजन का शौक़ हुआ करता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : हब्शी ग़ुलाम मस्जिद के प्रांगण में भालों-बरछियों और दूसरे हथियारों के चलाने का अभ्यास और युद्ध कला का प्रदर्शन करते। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ये खेल दिखाते रहते, यहाँ तक कि जब हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का जी भर जाता तो वे चली जातीं। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) नौजवान थीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बहुत अच्छी तरह समझते थे कि इस उम्र में स्त्रियों की भावनाएँ क्या होती हैं। वैध सीमाओं में रहते हुए स्त्रियों और विशेषतः कमसिन स्त्रियों की भावनाओं का ख़याल रखना आवश्यक है। इसका अनुमान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस आचरण से किया जा सकता है, जिसका उल्लेख इस हदीस में किया गया है।
अपने लोगों और मित्रों के साथ
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सम्बन्ध में कहते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बीमार का हाल पूछने जाते, जनाज़े के साथ जाते, अधीनस्थों और ग़ुलामों का निमन्त्रण स्वीकार कर लेते और गधे पर सवार हो लेते। (हदीस : बैहिक़ी, फ़ी शोअबिल-ईमान)
व्याख्या : इस हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है—
(i) बीमार की मिज़ाजपुरसी के लिए स्वयं जाते, सामान्य लोगों की तरह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी जनाज़े के साथ चलते और क़ब्रिस्तान पहुँचते।
(ii) लोगों के मध्य कोई अन्तर और विभेद न करते। अहंकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के यहाँ पाया ही नहीं जाता था। आप हरेक से प्रेम करते थे और हरेक के लिए उनके दिल में जगह थी। एक ग़ुलाम और अधीनस्थ भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को निमन्त्रण देता तो वे उसके निमन्त्रण को स्वीकार कर लेते थे।
(iii) गधे पर सवार होने से भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) परहेज़ न करते। शान-शौकत और अनावश्यक औपचारिकताओं से दूर रहते। दुनियादार शासकों जैसी कोई बात आपके यहाँ नहीं पाई जाती थी।
(2) हज़रत ख़ारिजा-बिन-ज़ैद-बिन-साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक बार लोगों का एक दल (मेरे पिता) ज़ैद-बिन-साबित के पास आया और उनसे कहा कि आप हमें रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कुछ हदीसें सुनाइए। उन्होंने कहा—
“मैं आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बिलकुल पड़ोस में रहता था। जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईश्वरीय वाणी का अवतरण होता तो मुझे बुला भेजते। मैं आप की सेवा में उपस्थित होकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेश से उसे लिखता। आप ऐसे थे कि जब हम दुनिया की चर्चा करते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी हमारे साथ दुनिया की चर्चा करते और जब हम परलोक की चर्चा करते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी हमारे साथ परलोक की चर्चा करते और जब हम खाने-पीने की चर्चा करते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी हमारे साथ उसकी चर्चा करते। यह प्रत्येक बात मैं तुम लोगों को रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बता रहा हूँ।" (हदीस : तिर्मिज़ी)
व्याख्या : हज़रत ज़ैद-बिन-साबित के इस कथन का कि 'मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पड़ोसी था' का मतलब यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वृत्तान्त और आपके दैनिक कार्य और आपके शील-स्वभाव आदि का ज्ञान दूसरों की अपेक्षा उन्हें अधिक है।
यह हदीस बताती है कि लोगों के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामाजिक सम्बन्ध और सम्पर्क अत्यन्त सुखद और सहज थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों की बातों में शामिल होते थे, चाहे उनका सम्बन्ध धर्म से हो या सांसारिक मामलों से। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऐसी बातचीत में अपने सहाबा का साथ देने से परहेज़ नहीं करते थे जिसमें कोई बुराई न होती। यद्यपि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मजलिसें मूलतः धार्मिक और ज्ञानपरक ही होती थीं और ज़रूरी और काम की बातों के अलावा व्यर्थ बातों से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी ज़बान को हमेशा सुरक्षित रखते थे।
यह हदीस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी हर तरह की बनावट और कृत्रिमता (Artificiality) से सर्वथा मुक्त थी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने सामाजिक जीवन में मानवीय और प्राकृतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करते थे। जिन बातों पर लोग आश्चर्य करते, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी आश्चर्य प्रकट करते और जिन बातों पर लोग प्रसन्नता प्रकट करते आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी उनपर प्रसन्न होते। मानव-स्तर से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने आप को कभी उच्च नहीं समझा और न कभी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कोई ऐसा ढंग अपनाया जिसका उद्देश्य यह रहा हो कि लोग अधिक से अधिक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रभावित हों और अधिक से अधिक उनका आदर करें। जो भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आता आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मेहरबान पाता।
(3) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सफ़र में क़ाफ़िले के पीछे चलते, कमज़ोरों को अपनी सवारी पर बिठा लेते और उनके लिए दुआ करते। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : यह था नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्नेह और प्रेम कि किसी की भलाई करते तो पूरी भलाई करते। बूढ़ों और कमज़ोरों को न केवल यह कि अपनी सवारी पर अपने साथ बिठा लेते, बल्कि उनके लिए दुआ भी करते कि उनको लोक और परलोक दोनों में सफलता और भलाई प्राप्त हो।
(4) हज़रत औफ़-बिन-मालिक अशजई (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि तबूक के युद्ध के अवसर पर मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस समय चमड़े के एक छोटे से तंबू में ठहरे थे। मैंने (बाहर से) सलाम किया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा—
“अन्दर आ जाओ।” इसपर मैंने निवेदन किया कि क्या मैं पूरा अन्दर आ जाऊँ? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “पूरे ही दाख़िल हो जाओ।" फिर मैं अन्दर दाख़िल हो गया। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : इस हदीस के एक उल्लेखकर्त्ता उसमान-बिन-अबी-अल-आतका का कहना है कि जिस ख़ेमे में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ठहरे हुए थे, वह एक छोटा-सा ख़ेमा था। इसलिए हज़रत औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि क्या मैं ख़ेमे में पूरे तौर पर आ जाऊँ, यानी ख़ेमा छोटा है, मैं इसमें पूरा आ भी सकता हूँ या नहीं।
इस हदीस से यह मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने सहाबा के साथ बेतकल्लुफ़ थे। यही कारण है कि सहाबा भी कभी-कभी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से विनोदपूर्ण बातें कर लेते थे।
(5) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि (जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीमार थे और इसी बीमारी में आपका देहान्त हुआ तो एक दिन) हज़रत अबू-बक्र और हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) अनसार की एक मजलिस के पास से गुज़रे। देखा कि वे रो रहे हैं। पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें अपने सिलसिले में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मजलिस याद आ गई। (यह सुनकर) उनमें से कोई साहब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुए और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इसकी सूचना दी। उल्लेखकर्त्ता का कथन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बाहर आ गए। उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चादर का एक कोना पट्टी के रूप में अपने सिर पर बाँधे हुए थे। फिर आप मिम्बर पर चढ़े और उसके बाद फिर कभी आपको मिम्बर पर चढ़ने का अवसर न मिल सका। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा की, फिर कहा—
“मैं तुम्हें अनसार के बारे में वसीयत करता हूँ (कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना), क्योंकि उनकी हैसियत मेरे आमाशय और मेरी गठरी की है। उनपर जो हक़ था, वे उसे अदा कर चुके और जो उनका हक़ है, वह अदा होना बाक़ी है। अतः उनके नेक लोगों का उज़्र स्वीकार करना और उनके बुरों के साथ क्षमा से काम लेना।" (हदीस : बुख़ारी)
व्याख्या : "अनसार की हैसियत मेरे आमाशय और मेरी गठरी की है" इसका आशय यह है कि अनसार मेरे विश्वासपात्र हैं। मैंने सभी मामलों में उनपर विश्वास किया है और उन्होंने मेरे विश्वास को कभी आघात नहीं पहुँचाया। वे मेरे राज़दार हैं। वे किसी दृष्टि से हमसे दूर नहीं हैं।
अनसार ने सत्यमार्ग में जान-माल, अर्थात प्रत्येक चीज़ से हमारा साथ दिया। हमारे प्रति उनकी हितैषिता में कभी भी किसी दौर में कोई कमी नहीं आई।
उन (अनसार) के प्रतिनिधियों ने मक्का में पहुँचकर लैलतुल-उक़बा में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हाथ पर इस्लाम की बैअ्त करते हुए अपनी ओर से जिस सहायता और सहयोग का वादा किया था, इतिहास साक्षी है कि यह वादा उन्होंने पूरा करके दिखा दिया।
अनसार के ज़िम्मे जो हक़ था, उसको तो उन्होंने ठीक-ठीक पूरा कर दिया। अब जो चीज़ बाक़ी है वह यह है कि अनसार के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। उनके साथ नरमी बरती जाए। उनके अच्छे लोग अगर अपनी किसी कोताही या भूल-चूक पर कोई उज़्र (विवशता) पेश करें तो उसे स्वीकार कर लिया जाए और यदि उनके कुछ लोगों से कोई ऐसी ग़लती हो जाए जिसके लिए वे कोई मजबूरी न प्रकट कर सकते हों तो उनके साथ क्षमा से काम लिया जाए। उनके साथ किसी तरह की कठोरता, अत्याचार और अन्याय करना उचित नहीं। अनसार ने जो क़ुरबानियाँ पेश की हैं, निश्चय ही ख़ुदा उन्हें परलोक में उन क़ुरबानियों का प्रतिफल और पुरस्कार प्रदान करेगा। परलोक में उनको अपने नबी का समीप्य और संग-साथ भी प्राप्त होगा।
किसी निर्धन के साथ
(1) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि गाँव का रहनेवाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम ज़ाहिर-बिन-हराम (रज़ियल्लाहु अन्हु) था। वह गाँव से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए उपहारस्वरूप कुछ (सब्ज़ी आदि) लाया करता था। जब वह वापस जाना चाहता तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसके लिए शहर का कुछ सामान साथ कर दिया करते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“ज़ाहिर, हमारा 'गाँव' है और हम उसका 'शहर' हैं।” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उससे प्रेम करते थे, हालाँकि वह एक कुरूप व्यक्ति था। एक दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) (बाज़ार) गए तो ज़ाहिर अपना सौदा बेच रहा था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पीछे से उसे गोद में ले लिया। वह आप को देख नहीं रहा था। उसने कहा, "मुझे छोड़ दो। यह कौन व्यक्ति है?” जब मुड़कर देखा तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहचान लिया। फिर वह पूरी कोशिश करने लगा कि अपनी पीठ को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सीने से चिमटाए रहे। इधर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आवाज़ लगाने लगे कि “कौन इस ग़ुलाम को ख़रीदता है?" ज़ाहिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुदा की क़सम, आप मुझे नाकारा पाएंगे। इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, "लेकिन ख़ुदा की दृष्टि में तुम नाकारा नहीं हो।” (हदीस : शरहुस्सुन्नह)
व्याख्या : “ज़ाहिर हमारा गाँव है और हम उसका शहर हैं" मतलब यह है कि वे हमें देहात की चीज़ें देते हैं और हम उनके लिए शहर की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं।
"कौन इस ग़ुलाम को ख़रीदता है", यह बात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विनोदस्वरूप कही लेकिन यह कोई झूठ भी न था, क्योंकि ज़ाहिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ख़ुदा के ग़ुलाम तो थे ही।
आपके इस कथन का कि “तुम नाकारा नहीं हो” का अर्थ होता है कि ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा बड़ा महत्व और मूल्य है। ईश्वर की दृष्टि में जिस व्यक्ति का महत्व हो उसे नाकारा नहीं कहा जा सकता।
बच्चों के साथ
(1) हज़रत जाबिर-बिन-समुरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने घरवालों के पास जाने के लिए (मसजिद से) बाहर निकले। मैं भी आपके साथ बाहर आया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने कुछ बच्चे आ गए। आपने उनमें से प्रत्येक के गाल पर हाथ फैरा। और फिर मेरे गालों पर भी आपने हाथ फैरा। उस समय मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हाथ को ऐसा ठण्डा और ख़ुशबूदार पाया मानो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हाथ को अभी इत्र के डिब्बे से निकाला हो। (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : इससे मालूम होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बच्चों से कितना अधिक प्यार करते थे और बच्चे भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बहुत प्यार करते थे।
(2) हज़रत बुरीदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे सामने ख़ुत्बा दे रहे थे कि अचानक हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) आ गए। दोनों लाल कुर्ते पहने हुए थे। वे इस तरह चले आ रहे थे कि (अल्पावस्था के कारण) गिर-गिर पड़ते थे। यह देखकर ख़ुदा के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मिम्बर से नीचे उतरे और उन दोनों को गोद में उठा लिया और फिर अपने सम्मुख उन्हें बिठाकर कहा—
“अल्लाह ने सच कहा है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो परीक्षा हैं।" मैंने इन बच्चों को देखा कि ये गिरते-पड़ते चले आ रहे हैं तो मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी बात रोककर उन्हें उठा लिया। (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)
व्याख्या : बच्चों और विशेषकर सन्तान से स्नेह रखना एक प्रिय कार्य है। इसलिए ख़ुत्बे को कुछ क्षण के लिए रोककर अगर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मासूम बच्चों को उठा लिया और उन्हें अपने सामने बिठा लिया तो यह कोई अनुचित बात न थी।
"मैंने बच्चों को गिरते-पड़ते आते देखा तो मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी बात को रोककर उन्हें उठा लिया।" यह बात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विनम्रता और विनीत भाव के कारण कही। इसके अतिरिक्त इसमें उपस्थित लोगों के लिए चेतावनी भी थी कि वे इसे कोई नियमित आचरण न बनाएँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (उपर्युक्त हदीस में) क़ुरआन के जिस अंश को पढ़ा वह क़ुरआन की सूरा-64, अत-तग़ाबुन की आयत 15 का एक अंश है।
(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैं दिन के एक हिस्से में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ बाहर निकला। जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के घर पहुँचे तो कहने लगे—
“क्या यहाँ मुन्ना है? क्या यहाँ मुन्ना है?” आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आशय हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से था (जिन्हें देखने आप वहाँ पहुँचे थे)। थोड़ी ही देर गुज़री होगी कि हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) दौड़ते हुए आ गए। दोनों ही एक-दूसरे के गले से लिपट गए। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “ऐ अल्लाह! मैं इससे मुहब्बत रखता हूँ। तू भी इससे मुहब्बत रख और उस व्यक्ति से भी मुहब्बत रख जो इससे मुहब्बत रखता हो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : यह हदीस बताती है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बच्चों से कितना अधिक प्रेम करते थे। इससे यह भी मालूम हुआ कि बच्चों को गले लगाना, उन्हें गोद में ले लेना और उन्हें प्यार करना और विशेष रूप से बच्चों से प्यार करना धर्म में प्रिय और उत्तम कर्म है। बच्चों के प्रति प्रेम और दया न दर्शाना दुर्भाग्य है। एक बार जब एक बद्दू व्यक्ति के मुँह से निकला कि हम तो बच्चों का चुम्बन नहीं लिया करते तो इसपर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“अल्लाह ने जब तेरे दिल से दयालुता निकाल ली तो मैं क्या कर सकता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
एक हदीस में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन उद्धृत किया गया है कि “अभागे ही के हृदय से दयालुता निकाल ली जाती है।” (हदीस : तिर्मिज़ी)
इस हदीस से उन शुष्क हृदय तपस्वियों के इस दृष्टिकोण का खण्डन होता है कि ईश्वर-प्रेमियों को बाल-बच्चों से कोई हार्दिक सम्बन्ध नहीं होता, बल्कि यथासम्भव वे उनसे दूर ही रहना पसन्द करते हैं। यह वास्तव में परहेज़गारों का नहीं बल्कि संन्यासियों का दृष्टिकोण और उनकी नीति है जो इस्लामी शिक्षाओं और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आचरण और आदर्श के सर्वथा प्रतिकूल है।
एक उल्लेखनीय बात इस हदीस से हमें यह भी मालूम होती है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिस किसी से प्रेम करते तो उसके लौकिक और पारलौकिक जीवन की भलाई के भी इच्छुक हो जाते थे। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस विशिष्ट भाव का प्रदर्शन विभिन्न शैलियों में होता था। अतएव इस हदीस में हम देखते हैं कि आपने अगर अपने नवासे (नाती) से स्नेह प्रदर्शित किया तो उनके लिए आपके मुँह से यह दुआ भी निकली कि “ऐ अल्लाह! तू इसे प्रिय रख।" लोक और परलोक में इससे बढ़कर कल्याण और भलाई की बात और क्या हो सकती है।
(4) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हम लोगों से अत्यन्त घुल-मिल जाया करते थे, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से (विनोदपूर्वक) कहते, “अबू-उमैर! नुग़ैर क्या हुआ?” उसके (मेरे भाई के) पास एक नुग़ैर था, जिससे वह खेला करता था और जो मर गया। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)
व्याख्या : अबू-उमैर हज़रत अनस के माँ शरीक छोटे भाई थे। उनके पिता का नाम अबू-तलहा ज़ैद-बिन-सुहैल अनसारी था।
नुग़ैर वास्तव में 'नुग़रुन' का लघु रूप है। 'नुग़्र' एक छोटे पक्षी का नाम है जिसकी चोंच लाल होती है। उसे सम्भवतः हमारे यहाँ 'लाल' कहते हैं। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) के भाई कब्शा (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस पक्षी को लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आए थे और वे इस चिड़िया के साथ खेला करते थे, जैसा कि बच्चों की आदत हुआ करती है। अचानक वह चिड़िया मर गई। उसके मरने के बाद जब कभी वह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आते तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) विनोदपूर्वक उन्हें छेड़ते और कहते, अबू-उमैर! तुम्हारे नुग़ैर का क्या हुआ? शाब्दिक अनुप्रास की दृष्टि से उन्हें उनके नाम के बजाए अबू-उमैर कहकर पुकारते थे।
(5) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“निस्सन्देह हसन और हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) मेरी दुनिया के दो फूल हैं।" (हदीस : बुख़ारी, तिर्मिज़ी)
व्याख्या : मूल हदीस में शब्द 'रैहान' प्रयुक्त हुआ है। शब्दकोश में 'रैहान' शब्द के कई अर्थ आए हैं, जैसे राहत, रहमत, आराम और सुख-चैन आदि। सुगन्धित घास और फूल को भी रैहान कहते हैं। बच्चों को रैहान इसलिए कहते हैं कि उनसे दिल को राहत और आँखों को ठंडक मिलती है। फूल की तरह बच्चों को भी लोग प्यार से सूँघते और चूमते हैं।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन का अर्थ यह है कि ख़ुदा दुनिया में लोगों को फूल जैसे बच्चे प्रदान करता है, जिनसे उन्हें हार्दिक सुख मिलता है। मेरी दुनिया के दो फूल, ये हसन और हुसैन हैं। अपने इन नवासों को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किस निगाह से देखते थे, इसका अन्दाज़ा इस हदीस से भली-भाँति किया जा सकता है।
(6) हज़रत अनस-बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कुछ बच्चों के पास से गुज़रे तो उनको सलाम किया और कहा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऐसा करते थे। (यानी बच्चों को आप सलाम करते थे।) (हदीस : बुख़ारी)
व्यवहार (Dealing)
(1) हज़रत साइब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। लोग मेरी चर्चा कर रहे थे और मेरी प्रशंसा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मैं इसे तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ।" मैंने निवेदन किया कि मेरे माँ-बाप की क़सम, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सच कहा। कारोबार में आप मेरे साझीदार थे। फिर क्या ही अच्छे साझीदार थे। न कभी धोखेबाज़ी से काम लेते थे और न झगड़ते थे। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : हज़रत साइब (रज़ियल्लाहु अन्हु) अज्ञानकाल में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साझे में कारोबार करते थे। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि मैं साइब को तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ।
आपके विषय में एक सहाबी की गवाही और उसका बयान यह है कि मैंने आपको बेहतर साझीदार पाया। आम तौर पर जब दो आदमी किसी कारोबार में साझीदार होते हैं तो उनके बीच सामान्यतः कोई न कोई शिकायत पैदा हो जाती है और बात लड़ाई-झगड़े तक पहुँच जाती है। लेकिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस प्रकार के झगड़ों से हमेशा अलग रहते थे। यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नैतिक उच्चता का स्पष्ट प्रमाण है।
(2) अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक ऊँट क़र्ज़ लिया। फिर उससे अच्छा ऊँट उसे दिया और कहा—
“तुममें सबसे अच्छे लोग वे हैं जो अच्छे तरीक़े से ऋण चुकाते हैं।" (हदीस : मुस्लिम)
व्याख्या : नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तंगदिल, कृपण और धन-दौलत के लोभी बिल्कुल न थे। मामलों में आप दानशीलता और दूसरों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाते थे। सहीह मुसलिम में हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि एक अवसर पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझसे पाँच औक़िया में एक ऊँट ख़रीदा। मैंने यह शर्त रखी कि मदीना नगर तक मैं इसपर सवारी करूँगा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मेरी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैं मदीना पहुँचने के बाद ऊँट लेकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक औक़िया और दिया और यह भी कहा, “ऐ जाबिर! तुमने मूल्य प्राप्त कर लिया?” मैंने कहा हाँ। आपने कहा, “मूल्य भी लो और ऊँट भी लो। मूल्य भी लो और ऊँट भी लो।” यह था आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दानशीलता और उदारता का हाल।
जानवरों पर दया
(1) हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने पिता के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक बार हम लोग यात्रा में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ थे। एक अवसर पर जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शौच के लिए गए तो हमने एक हुम्मरा चिड़िया को देखा, जिसके साथ दो बच्चे भी थे। हमने उसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। फिर हुम्मरा आई और अपने पंखों को धरती पर बिछाने और धरती से लगने लगी। इतने में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ गए और कहा—
“किसने इसके बच्चों को पकड़कर इसे बेचैन कर रखा है। इसके बच्चों को इसे लौटा दो।” फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने चींटियों के रहने की जगह देखी जिसको हमने जला डाला था। कहा, “किसने इन चींटियों को जलाया है?" हमने कहा कि हमने जलाया है? आप ने कहा, “ईश्वर के अतिरिक्त, जो अग्नि का भी मालिक है, किसी के लिए उचित नहीं कि वह अग्नि की यातना दे।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : 'हुम्मरा' एक छोटी चिड़िया का नाम है जिसका रंग लाल होता है। दोनों बच्चों के छिन जाने पर वह अत्यन्त बेचैन और विकल हो गई और इस प्रकार मानो वह अपने बच्चों की गिरफ़्तारी पर शिकायत और फ़रियाद कर रही हो। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया।
ईश्वर के अतिरिक्त किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वह किसी को आग की यातना दे। आपके यह कहने का अर्थ यह है कि ऐसी कठोर यातना देने का अधिकार केवल ईश्वर को है, जिसने आग पैदा की है और निश्चय ही वह परलोक में यह यातना उन अपराधियों को देगा जिन्होंने घोर अपराध किए होंगे। और अपराध की गम्भीरता ही के कारण उन्हें यह कठोरतम यातना दी जाएगी।
(2) हज़रत आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु), तीरन्दाज़, कहते हैं कि एक बार जब हम उनके पास अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास थे कि एक आदमी आया, जो चादर ओढ़े हुए था और उसके हाथ में कोई चीज़ थी, जिसे छिपा रखा था। उसने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! मैं वृक्षों के एक झुण्ड के क़रीब से गुज़रा तो मुझे वहाँ चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने उन्हें पकड़ लिया और उनको अपनी चादर में रख लिया। इतने में उनकी माँ आ गई और मेरे सिर पर चक्कर लगाने लगी। मैंने उसको दिखाने के उद्देश्य से (चादर हटा दी और) उन बच्चों को खोल दिया। वह उनपर आ पड़ी। मैंने उन सबको अपनी चादर में लपेट लिया। अब वे मेरे पास हैं।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, “इनको यहाँ रखो।” मैंने उन्हें वहाँ रख दिया (और चादर हटा दी), मगर उनकी माँ उनसे लिपटी ही रही। यह देखकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“क्या तुम्हें चिड़ियों के इन बच्चों के साथ इनकी माँ की ममता और दया को देखकर आश्चर्य होता है? सौगन्ध है उसकी जिसने मुझे सत्य के साथ भेजा है, अल्लाह अपने बन्दों पर उससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है जितना चिड़ियों के बच्चों की माँ अपने बच्चों पर मेहरबान है। तुम इन बच्चों को ले जाओ और जहाँ से तुमने इन्हें पकड़ा है, वहीं रख दो और इनकी माँ को इनके साथ छोड़ आओ।” अतएव वह आदमी उन सबको वापस ले गया। (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : मालूम हुआ कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दयाभाव केवल मनुष्यों तक ही सीमित न था, बल्कि चिड़ियों और जानवरों तक के साथ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का व्यवहार अत्यन्त दया और करुणा से भरा होता था।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की एक अभिलाषा
(1) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उल्लिखित है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा—
“मेरे सहाबा में से कोई व्यक्ति किसी के बारे में मुझ तक कोई (ऐसी) बात न पहुँचाए (जिससे उसकी बुराई प्रकट होती हो), इसलिए कि मैं यह पसन्द करता हूँ कि जब मैं घर से निकलकर तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा सीना साफ़ हो।” (हदीस : अबू-दाऊद)
व्याख्या : अर्थात किसी के बारे में मेरे दिल में कोई मलिनता और घृणा न हो और न कोई मेरी नज़र से गिरे और न मेरे दिल में किसी के प्रति नाराज़गी हो।
हदीस के विद्वानों ने लिखा है कि इस हदीस में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी इस अभिलाषा को प्रकट किया है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दुनिया से इस हाल में विदा हों कि आप अपने सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से राज़ी और ख़ुश हों। कितनी पवित्र अभिलाषा थी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की! पवित्र हृदय में पवित्र अभिलाषा और उत्तम भावनाओं के सिवा और हो भी क्या सकता था!
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
Subscribe Our You Tube Channel
Recent posts
-
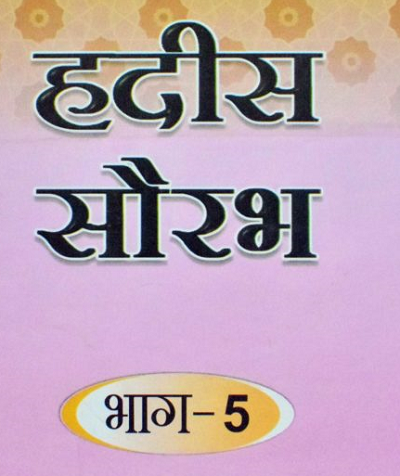
हदीस सौरभ भाग-5 (अनुवाद एवं व्याख्या सहित)
13 August 2024 -
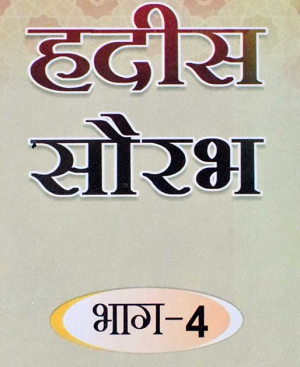
हदीस सौरभ भाग-4 (अनुवाद एवं व्याख्या सहित)
13 August 2024 -
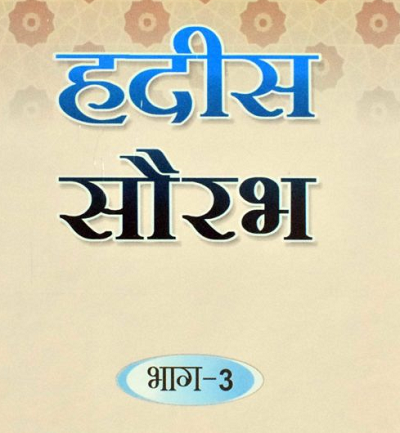
हदीस सौरभ भाग-3 (अनुवाद एवं व्याख्या सहित)
13 August 2024 -
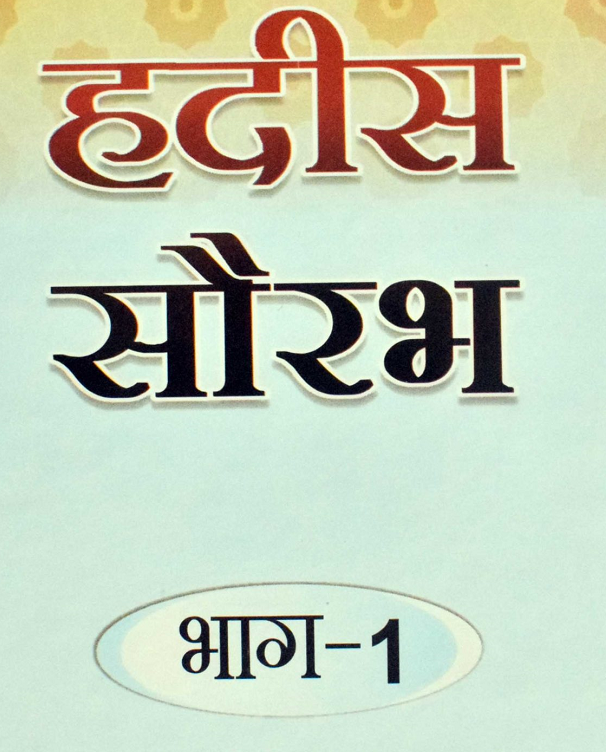
हदीस सौरभ भाग-1 (अनुवाद व व्याख्या सहित)
15 June 2024 -
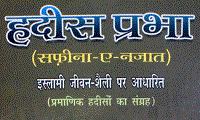
हदीस प्रभा
28 March 2024 -

उलूमे-हदीस : आधुनिक काल में (हदीस लेक्चर 12)
12 December 2023