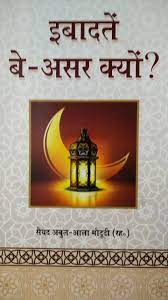
इबादतें बे-असर क्यों?
-
इस्लाम
- at 04 April 2022
सैयद अबुल-आला मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह)
प्रकाशक: मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स (MMI Publishers) नई दिल्ली
बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
“अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमवाला है।"
दो शब्द
क़ुरआन मजीद को अगर सरसरी तौर से भी पढ़ा जाए तो यह बात पहली नज़र में वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम इनसान की पूरी ज़िन्दगी को ख़ुदा के हुक्मों के मुताबिक़ गुज़ारने का नाम है। इसी लिए अल्लाह के तमाम पैग़म्बरों ने अपनी क़ौम से अपनी पूरी ज़िन्दगी में अल्लाह की फ़रमाँबरदारी करने का मुतालबा किया। यही मामला अल्लाह के आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर जो लोग ईमान लाए उनके दिमागों में यह बात बिलकुल वाज़ेह थी और उनकी अमली ज़िन्दगी इस हक़ीक़त की गवाह थी। ये पाकीज़ा लोग इस्लाम की मुकम्मल पैरवी किया करते थे। एक तरफ़ ये लोग इबादतों की पाबन्दी करते तो दूसरी तरफ़ दुनियावी मामलों में क़ुरआन व हदीस पर अमल करते। उनके कारोबार झूठ, फ़रेब और धोखेबाज़ी से पाक थे। झूठ, धोखा, बेईमानी, ख़यानत, चोरी और इन जैसी दूसरी ख़राबियों से दूर सच्चाई, अमानतदारी, हमदर्दी और लोगों की सेवा के रौशन चराग़ थे। इसलिए लोग इन मुसलमानों की ज़िन्दगी को देखकर इस्लाम से परिचित होते और उन्हें हक़ की गोद में आकर ही सुकून और चैन मिलता।
इन पाकीज़ा लोगों के बाद जो लोग आए उनमें यह कैफ़ियत बाक़ी नहीं रही और उन्होंने धीरे-धीरे इबादतों और ज़िन्दगी के दूसरे मामलों को एक-दूसरे से अलग कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि नमाज़, रोज़ा, ज़कात व हज की पाबन्दी करनेवाले बहुत-से लोगों के दुनियावी मामले इस्लाम की पाबन्दी से आज़ाद हो गए। उनमें वे बुराइयाँ पैदा हो गईं जिनको ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था।
इस हालत को देखकर फ़ितरी तौर पर बहुत से लोगों के दिमागों में ख़ुद इस्लामी इबादतों —नमाज़, रोज़ों वगैरा— ही के बारे में सवाल पैदा होने लगे कि आख़िर इन इबादतों की पाबन्दी क्यों की जाए और यह कि कहीं मुसलमानों की बदअमली और मामलों में उनकी ख़राबी की वजह ये इबादतें ही तो नहीं?
इस किताब में इसी सवाल का दलीलों के साथ बहुत ही असरदार जवाब दिया गया है। यह लेख मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी ने उर्दू माहनामा तर्जमानुल-क़ुरआन नवम्बर सन् 1935 ई. के अंक में 'नमाज़ के मुताल्लिक़ एक आम शुबहा' शीर्षक से लिखा था। यह लेख बाद में मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) के लेखों के संग्रह तफ़हीमात भाग-2 में शामिल किया गया। एक लम्बी मुद्दत गुज़र जाने के बाद भी इस लेख की अहमियत बाक़ी है, बल्कि आज इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस होती है। इसी लिए इस अहम और क़ीमती लेख को हिन्दी ज़बान में 'इबादतें बेअसर क्यों? के नाम से किताब की शक्ल में प्रकाशित किया गया है।
-नसीम ग़ाज़ी फ़लाही
इबादतें बे-असर क्यों?
हमारा एक लेख छपने के बाद हमें एक ख़त मिला जिसमें नीचे लिखे शुब्हा का इज़हार किया गया है—
“जहाँ तक नमाज़ों के वक़्तों का ताल्लुक़ है, आपने “हक़ गो" के शुब्हात (सन्देहों) को इस तरह दूर कर दिया है कि किसी बहस और गुफ़्तगू की गुंजाइश बाक़ी नहीं रही, लेकिन जहाँ आपने यह बताया है कि इनसान की अमली ज़िन्दगी पर नमाज़ का क्या असर पड़ता है, किस तरह नमाज़ इनसान को ख़ुदा के हुक्मों की इताअत और फ़रमाँबरदारी का आदी बनाती है और उसमें फ़र्ज़ पहचानने की सलाहियत पैदा करती और उसे ज़िन्दगी के मामलों में इस्लाम के डिसिप्लिन (अनुशासन) की पाबन्दी करने के क़ाबिल बनाती है, वहाँ एक शुब्हा पैदा होता है जिसका कोई जवाब मेरी समझ में नहीं आता। नज़रिए की हद तक तो मैं मानता हूँ कि नमाज़ और सिर्फ़ नमाज़ ही नहीं, इस्लाम की दूसरी फ़र्ज़ इबादतें भी इसी गरज़ के लिए रखी गई हैं कि इनसान की अमली ज़िन्दगी पर उनका असर पड़े और नज़र आए, और उनके लिए जो सूरत मुक़र्रर की गई है वह यक़ीनन ऐसी है कि उसका वही असर अख़लाक़, सीरत और किरदार पर नज़र आना चाहिए जो उसका मक़सद है। मगर इसकी क्या वजह है कि आज हम इस असर को मुसलमानों की अमली ज़िन्दगी में ग़ायब पाते हैं? चाहिए तो यह था कि नमाज़ पढ़नेवाले, रोज़ा रखनेवाले, हज और ज़कात अदा करनेवाले मुसलमान इस्लामी अख़लाक़ के नमूने होते, सच्चाई, अमानत, तक़वा, परहेज़गारी और पाकीज़गी के पुतले होते। मगर वाक़िआ (हक़ीक़त) इसके ख़िलाफ़ नज़र आता है। नमाज़ियों, रोज़ादारों और हाजियों को हम अख़लाक़ और मामलों के लिहाज़ से उन लोगों से कुछ भी अलग नहीं पाते जो नमाज़, रोज़ा और दूसरी इबादतों को छोड़े हुए हैं। बल्कि बहुत-से इबादत-गुज़ार लोगों का हाल तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने अपनी इबादत-गुज़ारी को अपने मामलों की ख़राबी के लिए ढाल बना रखा है और उनके कामों की ख़राबियों को देख-देखकर अकसर नए पढ़े-लिखे लोग ख़ुद नमाज़-रोज़े की तरफ़ से बदगुमान होते जा रहे हैं।"
इस ख़त में सवाल उठानेवाले ने जो शक ज़ाहिर किया है वह आजकल आमतौर पर दिलों में पाया जाता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक हद तक सच्चाई पर मबनी (आधारित) भी है, मगर इसमें कोई ऐसी मुशकिल या दिक़्क़त नहीं है जिसके हल करने में दुश्वारी हो। सवाल उठानेवाला ख़ुद मानता है कि इस्लामी इबादतों का नज़रिया अपनी जगह बिलकुल सही है। अक़्ल हुक्म लगाती है कि जिस ग़रज़ के लिए ये इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं वह इनसे मुकम्मल तौर पर पूरी होनी चाहिए। क्योंकि इनसान के नफ़्स (मन) को ख़ुदा की तरफ़ ध्यान दिलाने और ख़ुदा के हुक्मों के पालन का आदी बनाने के लिए इससे बेहतर कोई अमली तरीक़ा नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि हक़ीक़त की दुनिया में भी इस नज़रिए की सेहत साबित हो चुकी है। पहले ज़माने में इसी नमाज़-रोज़े और हज-ज़कात ने इस्लाम के अस्ली मक़सद के मुताबिक़ अरब और ग़ैर-अरब के लाखों-करोड़ों इनसानों की रूहानी और अख़लाक़ी तरबियत की थी और उनके अख़लाक़ सीरत और किरदार पर वही असर डाला था जो इस्लाम का ख़ास मक़सद था। अब अगर हम किसी आदमी या जमाअत की अमली ज़िन्दगी में इन इबादतों के वे असर नहीं देखते, तो इन इबादतों की तासीर में शक करने के बजाय हमको यह समझना चाहिए कि लोगों की असर लेने की सलाहियत किसी वजह से ख़राब हो गई है। हम जानते हैं कि आग लकड़ी को जला देती है। बार-बार देखने और तजरिबे में इस मामले में किसी शक की गुंजाइश बाक़ी नहीं रखी है कि आग का काम जलाना और लकड़ी का काम जल जाना है। इस यक़ीनी इल्म के बाद अगर किसी वक़्त हम यह देखते हैं कि लकड़ी को आग पर रखा जा रहा है और वह नहीं जलती तो हमें यह गुमान नहीं होता है कि आग में जलाने की ख़ासियत नहीं रही, बल्कि यह राय क़ायम करते हैं कि लकड़ी गीली है, इसमें आग का असर क़बूल करने की सलाहित नहीं है। बिलकुल इसी तरह जिस तरबियत के तरीक़े और हिदायत के बारे में अक़्ल के मुताबिक़ हम जानते हैं कि लोगों पर इससे एक ख़ास असर दिखना चाहिए और उसकी सही फ़ितरत इसी की माँग करती है कि इससे लोगों पर वही असर दिखे और तजरिबे से साबित भी हो चुका है कि मुख़्तलिफ़ ज़मानों में और मुख़्तलिफ़ हालतों में बेशुमार लोगों पर सचमुच वही असर पड़ा और दिखा है। इसकी तासीर और असर को अगर हम कुछ लोगों के हक़ में नाकाम देखते हैं तो क्या वजह कि हमारे दिल में इसकी तासीर के बारे में कोई शक पैदा हो? क्यों न हम यह समझें कि गीली लकड़ी की तरह उन लोगों में भी असर क़बूल करने की सलाहियत नहीं है?
जहाँ तक नमाज़ की ज़ाहिरी सूरत का ताल्लुक़ है, वह तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि मुक़र्रर किए गए वक़्तों पर कुछ जिस्मानी हरकतों का दोहराना और कुछ मुक़र्रर लफ़्ज़ों को बार-बार पढ़ना या दोहराना है। और यही हाल दूसरी इबादतों का भी है। एक ख़ास महीने में सुबह से शाम तक खाने-पीने और सोहबत (संभोग) से रुका रहे, इसका नाम रोज़ा हो गया। साल में एक बार अपने माल में से एक मुक़र्रर मिक़दार ख़ास ख़र्चों के लिए निकाल दी, यह ज़कात हो गई। एक ख़ास ज़माने में मक्का-मदीना का सफ़र कर लिया और ख़ास मक़ाम पर कुछ मनासिक (हज के अरकान) अदा कर दिए, यह हज हो गया। ज़ाहिर है कि बजाए ख़ुद इन कामों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनसान के नफ़्स पर असर डाल सकती हो। सिर्फ़ एक काम होने के लिहाज़ से नमाज़ और एक जिस्मानी वरज़िश, रोज़े और फ़ाक़े, ज़कात और सरकारी टैक्स, हज और आम सफ़रों के बीच कुछ भी फ़र्क नहीं। और कोई अक़्लवाला इनसान यह नहीं कह सकता कि जिस्मानी वरज़िश से रूह में पाकीज़गी पैदा होती है, या फ़ाक़ा करने से अख़लाक़ी तरबियत होती है, या टैक्स अदा करने और किसी मक़ाम का सफ़र कर आने से इनसान में ऊँचे दर्जे की ख़ूबियाँ पैदा होती हैं।
मगर जो चीज़ इन कामों को दूसरे कामों से मुमताज़ (अलग) करती और इनको अख़लाक़ी तहज़ीब, नफ़्स का तज़किया (पाकी) और रूह की पाकीज़गी का एक बेहतरीन ज़रिआ बनाती है, वह ईमान है। ईमान ही रुकू व सजदों और क़ियाम व कुऊद (यानी झुकने, माथा टेकने और खड़े होने, बैठने) को “नमाज़' बनाता है। वही फ़ाक़े को “रोज़े" में बदल देता है, वही टैक्स की कैफ़ियत में इन्क़िलाब पैदा करके इसे "ज़कात' का बुलन्द मर्तबा अता करता है और वही एक ख़ास क़िस्म के सफ़र को सैरो-तफ़रीह की गिरी-पड़ी जगह से उठाकर “हज" के सबसे ऊँचे मक़ाम पर पहुँचा देता है। अस्ल में इन तमाम इबादतों की रूह और इनका जौहर वही है। इसी से इबादत के अरकान में मानवीयत (सार्थकता) पैदा होती है। वही इन अरकान को तासीर (असर) की ताक़त देता है। उसी की बदौलत नफ़्स (मन) में इनसे मुतास्सिर होने की ताक़त और सलाहियत पैदा होती है।
अब ज़ाहिर है कि अगर कोई आदमी सचमुच ईमान रखता हो, ख़ुदा को अपना ख़ुदा समझता हो, आख़िरत की ज़िन्दगी पर अक़ीदा रखता हो, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को ख़ुदा का रसूल मानता हो और उनकी लाई हुई तालीम को ख़ुदा की तालीम समझता हो तो मुमकिन नहीं है कि वह दिन में पाँच वक़्त नमाज़ का सबक़ ताज़ा करे और फिर भी उसका दिल उस सबक़ के असर से बिलकुल ख़ाली रहे, और उसकी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में ख़ुदा का डर और ख़ुदा के हुक्मों की इताअत का कोई निशान नुमायाँ न हो। हर साल पूरे एक महीने तक सख़्त ज़ाब्ते की पाबन्दी के साथ परहेज़गारी और ख़ुदातरसी व फ़रमाँबरदारी की तरबियत पाता रहे और फिर भी उसकी ज़िन्दगी में बिलकुल ही कोई इन्क़िलाब न पैदा हो, यहाँ तक कि वह बिलकुल ऐसा कोरा-का-कोरा रह जाए कि मानो उसने कोई तरबियत पाई ही नहीं। ख़ालिस ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान की वजह से हर साल अपने मनपसन्दीदा माल की क़ुरबानी करता रहे और फिर भी मन की कठोरता और बेरहमी और हरामख़ोरी व ख़ुदग़र्ज़ी के मर्ज़ में मुब्तला रहे जो एक बेईमान, ख़ुदपरस्त और स्वार्थी इनसान में पाई जाती है। अपने पालनहार रब की पुकार पर लब्बैक-लब्बैक (मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ) कहता हुआ अपना घर-बार छोड़कर और अपने फ़ायदे व पसन्द के काम छोड़ करके फ़क़ीरों के से लिबास पहनकर निकले, एक लम्बी मुद्दत तक इसी शौक़ और इश्क़ की लगन दिल में लिए हुए सफ़र करे, यहाँ तक कि इस्लाम के मर्कज़ (केन्द्र) में पहुँचकर अपनी आँखों से अल्लाह की उन रौशन निशानियों को देख ले जो ख़ुदा के सच्चे और फ़रमाँबरदार बन्दों की सरफ़राज़ियों पर और सरकशों की नामुरादियों पर खुली गवाही दे रही हैं, और फिर भी जब वापस आए तो उस सफ़र के आसार और नतीजों से उसकी सीरत ऐसी ख़ाली हो कि वह मानो कहीं गया ही नहीं और उसकी आँखों ने कुछ देखा ही नहीं।
यह ज़रूर है कि मिक़दार और कैफ़ियत के लिहाज़ से हर आदमी पर इन इबादतों की तासीर एक जैसी नहीं हो सकती। लोगों की कम-ज़्यादा सलाहियतों के लिहाज़ से, और ईमानी क़ुव्वत की ज़्यादती और कमी के लिहाज़ से इनका कमो-बेश और शदीद और कमज़ोर होना एक फ़ितरी बात है। लेकिन यह किसी तरह मुमकिन नहीं है कि ईमान के साथ जो इबादत की जाए वह बिलकुल ही बेअसर साबित हो। हम यह बात पूरे यक़ीन के साथ कह सकते हैं कि जो आदमी नमाज़ को गन्दी बातों और बुराइयों के साथ जमा करता है, जिसकी ज़िन्दगी में रोज़ा और गुनाह एक साथ पाए जाते हैं, जिसकी सीरत और अमल में हरामख़ोरी और ज़कात दोनों एक साथ मौजूद हैं, जो हज और दीनी हुरमतों (मर्यादाओं) के अनादर को एक-दूसरे के साथ मिला रहा है, उसकी नमाज़, “नमाज़' नहीं, एक आदी हरकत है, उसका रोज़ा, “रोज़ा" नहीं फ़ाक़ा है, उसकी ज़कात, “ज़कात” नहीं चन्दा या टैक्स है, उसका हज, “हज” नहीं, बल्कि उसके हक़ में वैसा ही एक सफ़र है जैसा पेरिस और लन्दन का सफ़र।
यह जो कुछ कहा गया है, यह सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर चस्पाँ होता है जिनकी सीरत (जीवन-चरित्र) और किरदार पर, सवाल करनेवाले के बयान के मुताबिक़, इस्लामी इबादतों का कोई असर दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे यह तस्लीम करने से बिलकुल इनकार है कि मुसलमानों में जितने नमाज़ी, रोज़ोदार, ज़कात के पाबन्द और हज अदा करनेवाले हैं, सब-के-सब ऐसे ही हैं। मुमकिन है कि एक कम तादाद ऐसे मुनाफ़िक़ों की भी हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर का यह हाल नहीं है। ज़्यादातर लोग जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं वह मुनाफ़िक़त (कपटाचार) नहीं, बल्कि ईमान की कमज़ोरी है। इसी कमज़ोरी का यह नतीजा है कि इबादतों की तासीरें भी कमज़ोर हो गई हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और हज करते हैं, मगर ये सब चीज़ें दिलों को छूती हुई इस तरह गुज़र जाती हैं कि जैसे भाप आईने की सतह पर एक हल्की-सी नमी छोड़कर गुज़र जाए। यह तासीर (असर) का न होना नहीं, बल्कि उसकी कमज़ोरी है। ईमान की चिंगारियाँ दिलों में दबी-छिपी अब भी मौजूद हैं, और उनकी हरारत (गर्मी) से इबादतें कुछ-न-कुछ असर ज़रूर कर रही हैं, लेकिन वह असर इतना कमज़ोर होता है कि इबादत करनेवालों की सीरत और किरदार में उसके निशानात कुछ बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं होते।
मैं यह मानने से भी इनकार करता हूँ कि मुसलमानों में जो लोग इबादत के पाबन्द हैं उनका हाल इबादत न करनेवालों से बदतर या उनके बराबर है। सच्ची बात यह है कि हमारी क़ौम में अब भी अगर मजमूई हैसियत से देखा जाए तो अख़लाक़ी हैसियत से वही हिस्सा ज़्यादा बेहतर पाया जाएगा जो नमाज़-रोज़े का पाबन्द है। मगर अस्ल मामला यह है कि देखनेवालों की निगाहों में ख़ुदा-फ़रामोश लोगों की बनिस्बत इबादतगुज़ारों की बुराइयाँ ज़्यादा खटकती हैं। एक नमाज़-रोज़ा के छोड़नेवाले की बदकिरदारी और मामलों की ख़राबी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं मालूम होती जितनी एक नमाज़-रोज़े के पाबन्द की बदकिरदारी और मामले की ख़राबी। बे-नमाज़ी से बुराई ही की उम्मीद होती है इसलिए जब वह बुराई करता है तो उसकी कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं होती। मगर नमाज़ी से हर आदमी उम्मीद रखता है कि वह ख़ुदा से डरनेवाला और परहेज़गार होगा। इसलिए जब उससे आम उम्मीदों के ख़िलाफ़ बुरे काम अमल में आते हैं तो यह मामला हर आँख में खटक और हर ज़बान पर शिकायत पैदा कर देता है। सफ़ेद दीवार पर स्याही की एक छींट भी हो तो हर देखनेवाला उस ऐब पर उँगली उठाएगा। बावरचीख़ाने की स्याह (काली) दीवारों पर जितना चाहे कोयला मल दीजिए, किसी को भी उसकी परवाह न होगी।
हद से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बयान न किया जाए तो हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी है कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे नमाज़ियों और इबादत-गुज़ारों और हाजियों की है जो इन इबादतों से अपने इस्लाहे-नफ़्स (मन के सुधार) के वह पूरे फ़ायदे हासिल नहीं कर रही है जो अस्ल में उसे हासिल हो सकते हैं। और यह बात कुछ बे-वजह नहीं है। इसकी एक ख़ास वजह है और वह यह है कि 'ईमान' जो इन इबादतों की जान और इनकी तासीर का अस्ल सबब था, दिलों में कमज़ोर हो गया है।
फिर ईमान की कमज़ोरी की भी एक वजह है। और वह है क़ुरआन की तालीम से अनजान होना। ख़ुदा ने ईमान की दावत देने के लिए जिस चीज़ को ज़रिआ बनाया था वह तो यही क़ुरआन था। मगर आम मुसलमान इसकी समझ से महरूम और इसी की तालीम से नावाक़िफ़ हैं। अब आख़िर दिलों में ईमान का नशोनुमा हो तो किस तरह।
एक और चीज़ जिसका हमारी इबादतों को कमज़ोर असरवाली बनाने में बड़ा हिस्सा है दीन और दुनिया के अलग-अलग होने का ग़लत और झूठा ख़याल है। यह अस्ल में जाहिलियत का अक़ीदा था, जिसको इस्लाम ने बिलकुल मिटा दिया था। मगर न मालूम इसने किस तरह मुसलमानों में राह पा ली। जाहिलियत के ज़माने में लोग यह समझते थे कि दीन इस्लामी ज़िन्दगी के शोबों में से सिर्फ़ एक शोबा (विभाग) है, जिसका दूसरे शोबों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मज़हबी रस्में, इबादतें और क़ुरबानियाँ सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी हैं कि ख़ुदा या देवताओं को ख़ुश किया जाए और ज़िन्दगी के मामलों में उनकी ताईद (समर्थन) हासिल की जाए। इन फ़र्ज़ों को अंजाम देकर जब इनसान इबादतगाहों से बाहर निकले तो मज़हब की तरफ़ से उसपर कोई ज़िम्मेदारी लागू नहीं होती और वह आज़ाद होता है कि अपनी दुनिया के मामले जिस ढंग पर चाहे चलाए।
इस्लाम ने इस ग़लत हदबन्दी को मिटाया। दीन को ज़िन्दगी का एक शोबा (विभाग) नहीं बल्कि पूरी ज़िन्दगी का अमली निज़ाम क़रार दिया। अक़ीदों और अख़लाक़ के बीच, ईमान और सीरत (जीवन-चरित्र) के बीच, इबादतों और मामलों के बीच, मज़हबी कामों और दुनियावी कामों के बीच एक गहरा ताल्लुक़ क़ायम किया। फिर इनसान की दुनियावी ज़िन्दगी ही को पूरी तरह दीनी ज़िन्दगी बना दिया। उसने बताया कि दीन इस दुनिया के मामलों से अलग कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इसी दुनिया के कारोबार में अल्लाह के क़ानून की पैरवी, उसके मुक़र्रर किए हुए हुदूद (सीमाओं) की पाबन्दी और उसकी रिज़ा (ख़ुशनूदी) की इताअत और पैरवी का नाम दीन है। इबादतें और मामले दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि मामले ही में अल्लाह की हदों की पाबन्दी और अल्लाह की ख़ुशनूदी की तलब व चाह और अल्लाह से क़ुरबत बढ़ाने की कोशिश का नाम इबादत है। नमाज़, रोज़े, हज, ज़कात को इबादत और फ़र्ज़ क़रार देने का यह मक़सद नहीं है कि इबादत को इन्हीं कामों (अमलों) में महदूद कर दिया जाए, बल्कि अस्ल में ये काम इनसान को उस बड़ी इबादत के लिए तैयार और आमादा करनेवाले हैं जिसका दायरा उसकी पूरी ज़िन्दगी पर फैला हुआ है। मुसलमानों की इबादतगाह पूरी कायनात है। उसकी सारी ज़िन्दगी इबादत है। उसको हर पल ख़ुदा का इबादतगुज़ार बन्दा होना चाहिए। उसकी इबादत की जगह सिर्फ़ उसकी मस्जिद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मस्जिद उसकी तरबियतगाह है जहाँ वह इबादत की क़ाबिलियत पैदा करता है। अगर उसकी नमाज़ और उसके रोज़े और उसकी दूसरी इबादतों का राबिता उसके मामलों से कट जाए और वह अपनी ज़िन्दगी के कामों में ख़ुदा के क़ानूनों की पाबन्दी से आज़ाद हो तो सिर्फ़ नमाज़-रोज़े की पाबन्दी से वह दीनदार और इबादतगुज़ार बन्दा नहीं बन सकता।
बड़े दुख और अफ़सोस की बात है कि दीन का यह ख़याल धीरे-धीरे मुसलमानों के ज़ेहन से मिटता चला जा रहा है और दीन-दुनिया के अलग-अलग होने का वही जाहिली ख़याल उसकी जगह ले रहा है जिसको इस्लाम ने पूरी तरह मिटा दिया था। यह इसी ग़लत ख़याल का नतीजा है कि इबादतों और मामलों का आपसी ताल्लुक़ टूट गया है। अमली ज़िन्दगी से नमाज़ों का राबिता टूट गया। माली (आर्थिक) मामलों पर ज़कात की फ़रमाँरवाई बाक़ी न रही। साल के ग्यारह महीने रमज़ान की हुकूमत से आज़ाद हो गए, बल्कि बरकतवाला रमज़ान ग़रीब ख़ुद भी अपनी हदों में सिर्फ़ हलक़ का दरबान बनाकर रख दिया गया। हज की हैसियत हिन्दुओं की यात्रा और ईसाइयों के Pilgrimage (पिलग्रिमेज) से ज़्यादा न रही। और यह ग़लतफ़हमी आमतौर पर लोगों में फैल गई (या फैला दी गई) कि नमाज़ और बेहयाई व बुराई, रोज़े और नाफ़रमानी व बिगाड़, ज़कात और हरामख़ोरी, हज और दीनी हुरमतों (मर्यादाओं) का अनादर साथ-साथ चल सकते हैं।
(पहली बार प्रकाशित: मासिक तर्जुमानुल-क़ुरआन, नवम्बर 1935 ई.)
(E Mail: HindiIslamMail@gmail.com Facebook: Hindi Islam , Twitter: HindiIslam1, You Tube: HindiIslamTv )
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
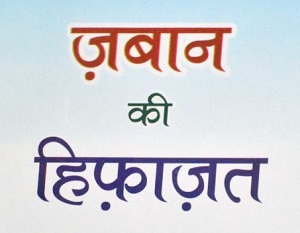
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
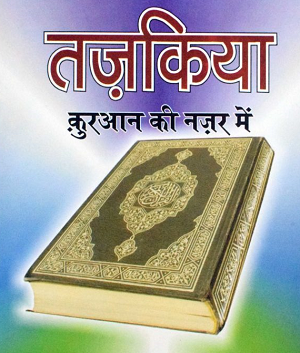
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

