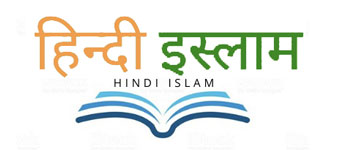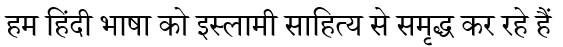मिल्लते इस्लामिया का संक्षिप्त इतिहास भाग-1
-
इतिहास
- at 19 June 2024
इतिहास की यह पुस्तक पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं इतिहासकार सरवत सौलत साहब ने उस दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी है, जो उद्देश्यपूर्ण और सैद्धान्तिक है। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात से ऊपर उठकर, मानव मात्र की प्रगति एवं विकास के उद्देश्य को सामने रखकर घटनाओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और नतीजे निकाले जाते हैं। उस किताब का आसान हिन्दी अनुवाद पेश है। यह अनुवाद सहज एव सरल रखा गया है। और इसमें जिन ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों के नाम आए हैं उन्हें विशुद्ध रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसके लिए बिरादरम ख़ालिद निज़ामी साहब ने जो सतर्कता दिखाई है और उन्होंने जो परिश्रम किया है वह अत्यन्त सराहनीय है। आशा है कि हम सब इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन!
लेखक : सरवत सौलत
अनुवादक : मुनाज़िर हक़
प्रकाशक : मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स
अपनी बात
इतिहास लेखन के तीन दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण वस्तुपरक अध्ययन का है अर्थात घटनाओं और परिस्थितियों को ज्यों का त्यों पेश कर दिया जाए, इसमें न कोई कमी की जाए न कोई बढ़ोतरी। दूसरा दृष्टिकोण जातिवादी अथवा राष्ट्रवादी है अर्थात घटनाओं एवं परिस्थितियों को जाति विशेष अथवा राष्ट्र विशेष के समर्थन में रखकर परिणाम निकाले जाएँ। तीसरा दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और सैद्धान्तिक है। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात से ऊपर उठकर, मानव मात्र की प्रगति एवं विकास के उद्देश्य को सामने रखकर घटनाओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और नतीजे निकाले जाते हैं।
पहला दृष्टिकोण विशुद्ध ऐतिहासिक होने के बावजूद उद्देश्यविहीन होने के कारण विशेष लाभप्रद नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण हालाँकि दुनिया के 95 प्रतिशत इतिहासकारों का प्रिय दृष्टिकोण है, परन्तु यह अपने पढ़नेवालों को जाति विशेष अथवा राष्ट्र विशेष की महानता की (अधिकतर झूठी) गाथा तो सुना सकता है, उन्हें वर्तमान एवं भविष्य के लिए कोई संबल नहीं प्रदान कर सकता। कारण?
कारण यह है कि यह दृष्टिकोण अपनी जाति अथवा राष्ट्र से प्रेम एवं अन्य जाति अथवा राष्ट्र से घृणा एवं विद्वेष के आधार पर खड़ा होता है। इसी दृष्टिकोण ने दुनिया को जातिगत अत्याचार, अन्याय, रक्तपात एवं विद्वेष का तोहफ़ा दिया है। अधिकतर दुष्टों को सज्जन इसी ने बनाया और अधिकतर सज्जनों पर लांछन इसी ने लगाए हैं। यह दृष्टिकोण विकसित होकर आज इस सीमा को पहुँच गया है कि अब जातीय स्वार्थ के लिए इतिहास तक गढ़े जाते हैं। इस दृष्टिकोण को माननेवाले इतिहासकारों की सशक्त लेखनी इतिहासविहीन क़ौमों का गौरवशाली इतिहास रच रही है।
रहा तीसरा दृष्टिकोण तो इतिहास लेखन का यही सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। विशेष कर इस्लामी इतिहास के लिए तो इसके अतिरिक्त और कोई दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता। इस्लाम एक विचारधारा है, एक आन्दोलन है जो विश्व की तमाम जातियों एवं राष्ट्रों के लिए है और लगभग विश्व की तमाम जातियों ने इसे स्वीकार भी किया है। अत: जातिवादी अथवा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के तहत इस्लामी इतिहास के साथ इनसाफ़ संभव नहीं। ख़ुद इस्लाम में 'क़ौमपरस्ती' की इजाज़त नहीं है। तात्पर्य यह कि एक अच्छा इस्लामी इतिहास उद्देश्यपूर्ण और सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के तहत ही लिखा जा सकता है।
इतिहास की यह पुस्तक पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं इतिहासकार सरवत सौलत साहब ने इसी अन्तिम दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी है। इस किताब का आसान हिन्दी अनुवाद पेश किया जा रहा है। यह अनुवाद सहज एव सरल रखा गया है। और इसमें जिन ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों के नाम आए हैं उन्हें विशुद्ध रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसके लिए बिरादरम ख़ालिद निज़ामी साहब ने जो सतर्कता दिखाई है और उन्होंने जो परिश्रम किया है वह अत्यन्त सराहनीय है। आशा है कि हम सब इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन!
प्रयास किया गया है कि इस पुस्तक में कोई ग़लती न रहे, फिर भी अगर पाठक कोई ग़लती पाएं तो हमें अवश्य सूचित करें ताकि सुधार किया जा सके।
-प्रकाशक
'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'
(अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है।)
प्राक्कथन
तारीख़े इस्लाम (इस्लाम का इतिहास) आम पारिभाषिक शब्दों के अनुसार किसी 'क़ौम' का इतिहास नहीं है, बल्कि एक आन्दोलन का इतिहास है और एक दृष्टिकोण के उत्थान एवं पतन की गाथा है। यदि हम इस्लामी इतिहास को गिरोह या जमाअत से सम्बद्ध करें तो इस गिरोह या जमाअत के लिए क़ौम' की बजाए 'मिल्लत' का शब्द ज़्यादा सही होगा। इसमें संदेह नहीं कि 'मिल्लत' शब्द हमारे यहाँ 'क़ौम' के अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा है, परन्तु इस्लामी चिन्तकों ने हमेशा इसकी व्याख्या की है कि राजनीतिक परिभाषा के रूप में 'क़ौम' या 'मिल्लत' का अर्थ मुसलमानों के निकट वह कभी नहीं रहा जो पश्चिम एवं अन्य क़ौमों में समझा जाता है।
अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर
ख़ास है तरकीब में क़ौमे रसूले हाशिमी —इक़बाल
या
निराला सारे जहाँ से इसको अरब के मेअमार ने बनाया
बिना हमारे हिसारे मिल्लत की इत्तिहादे वतन नहीं है —इक़बाल
इतिहास का एक विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है कि इस्लामी इतिहास एक वैचारिक संघर्ष का इतिहास है। जब भी इस्लामी उसूलों पर कार्यान्यवन में कमज़ोरी का आभास हुआ तो मुसलमान हुक्मरानों एवं समाज सुधारकों ने तुरन्त उस कमज़ोरी को समाप्त करने का प्रयास किया। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से लेकर औरंगज़ेब (रहमतुल्लाह अलैह) तक यही संघर्ष दृष्टिगोचर होता है।
इस्लामी इतिहास के इस अर्थ के निर्धारण के बाद कि यह एक विचारधारा का इतिहास है एक इतिहासकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह 'मिल्लते इस्लामिया' के इतिहास का अध्ययन उन्हीं उसूलों की रौशनी में करे जिनपर मिल्लते इस्लामिया की बुनियाद है और वह यह देखे कि मुसलमान कहाँ-कहाँ इन उसूलों पर चलते रहे और कहाँ-कहाँ उन्होंने इन उसूलों से मुख मोड़ा।
यहाँ हमारे इतिहास लिखने के रुझान की ओर संकेत कर देना अनुचित नहीं होगा। हमारे इतिहासकार प्रायः हर उस कारनामे को सराहने लगते हैं जो असाधारण कोटि के होते हैं। वे इसका ख़याल नहीं रखते कि एक मुसलमान की हैसियत से हमारे निकट उस कारनामे का कितना महत्त्व है। इतिहास लेखन की इस शैली का यह परिणाम हुआ कि तैमूर और नादिर भी उस पंक्ति में आ गए हैं जिसमें सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन हैं। आधुनिक काल के इतिहास में यह त्रुटि विशेष रूप से स्पष्ट हो गई है। हर वह व्यक्ति जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद या ग़ैर मुस्लिम शक्तियों का मुक़ाबला किया वह हमारा अनुकरणीय 'हीरो' बन गया है। इस प्रकार हर वह मुसलमान सम्माननीय हो जाता है जो भौतिकवादी जीवन के किसी भी पहलू में असाधारण विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। इस मामले में इस्लाम के मापदण्ड' को हमने तक़रीबन भुला दिया है। दरअसल हमारा दृष्टिकोण 'इस्लामी' की बजाए 'क़ौम परस्ताना' (जातिगत) होता जा रहा है। चूँकि इस दृष्टिकोण से हर उस कारनामे को सराहा जाता है जो ग़ैर क़ौम के मुक़ाबले में अंजाम दिया गया हो इसलिए हम भी ऐसा ही करने लगे हैं, परन्तु यह एक पश्चिमी और ग़ैर इस्लामी दृष्टिकोण है। इस कारण इस्लामी दृष्टिकोण को जो अच्छे और बुरे के बीच अन्तर करने का हमारे लिए सबसे बड़ा मापदण्ड है, नुक़सान पहुँच रहा है। आधुनिक काल के इतिहास में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उभर गया है और इसका परिणाम यह निकला है कि हर पुरानी बात और पुरानी रीति-रिवाज की निंदा की जाती है और हर नए बदलाव एवं हर नए आन्दोलन का उल्लेख उत्साहवर्धक अंदाज़ में किया जाता है। आलोचना करते समय हम यह बात बिलकुल भूल जाते हैं कि आधुनिक काल के बहुत-से नए आन्दोलन अपने साथ ग़ैर इस्लामी प्रभावी तत्त्व भी ला रहे हैं जिनके कारण हमारे समाज में इस प्रकार ग़ैर इस्लामी धारणाएँ, विचारधाराएँ और रीति-रिवाज विकसित होने लगे हैं जिस प्रकार प्राचीन काल की विभिन्न भाषाओं में ग़ैर इस्लामी मान्यताएँ एवं रीति-रिवाज हमारे समाज में प्रवेश कर गए थे। इस सोच का एक हास्यास्पद परिणाम यह निकला है कि बहुत-सी वही बातें जो हमारे प्राचीन काल के कारनामे गिनी जाती हैं और जिनपर पश्चिमी आलोचकों की आपत्तियों का हमारे विद्वान जवाब देते रहे हैं, वही बातें वर्तमान काल में ख़ुद हमारे अपने लेखक भाइयों के हाथों से जाने-अनजाने निन्दनीय घोषित की जा रही हैं। हमारे आधुनिक इतिहास लेखकों के लेखन का यह विरोधाभास बड़ा हानिकारक साबित हो रहा है और इसके कारण मुसलमानों में इस्लाम से सम्बन्धित संदेह और अविश्वास बढ़ता जा रहा है।
एक और वास्तविकता जो इस्लामी इतिहास के अध्ययन से मालूम होती है यह है कि मिल्लते इस्लामिया चूँकि बुनयादी रूप से एक ही संस्कृति और एक ही सभ्यता का ध्वजावाहक है इसलिए हम मिल्लत के इतिहास के विभिन्न हिस्सों को एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इस्लामी इतिहास को सही रूप में समझने के लिए इस्लामी इतिहास के केवल एक काल का अध्ययन पर्याप्त नहीं हो सकता और न ही किसी एक देश के इतिहास से हम इस्लामी सभ्यता एवं संस्कृति तथा विचारधारा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुसलमानों के उत्थान एवं पतन, उनके सामुदायिक जीवन तथा उनकी मान्यताओं एवं वैचारिक संघर्ष को किसी एक काल के संदर्भ में नहीं बल्कि उनके सम्पूर्ण इतिहास के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। विश्व इतिहास में इस्लामी काल के महत्त्व और उसके स्थान का उचित निर्धारण भी केवल इसी प्रकार किया जा सकता है। इस्लामी इतिहास की इस विशेषता को हमारे उत्थान काल के इतिहासकारों ने हमेशा स्वीकार किया है। 'तबरी' से लेकर 'तारीख़े अलफ़ी' तक प्रथम एक हज़ार साल में जिस प्रकार प्रमुख इतिहास लिखे गए हैं उनका विषय सम्पूर्ण इस्लामी इतिहास रहा है। यह केवल पतन काल ही है जिसमें हम राजनैतिक बिखराव के साथ-साथ सभ्यता एवं संस्कृति के ह्रास में भी फँस गए। अब जबकि मुसलमानों के पुनर्जागरण का प्रारंभ हो चुका है, हमारे लिए अपनी ऐतिहासिक एवं सभ्यता जन्य एकता को बहाल करना अत्यन्त आवश्यक है।
ये थे वे चन्द उसूल जिनके अनुसार मैंने अब से कोई पन्द्रह वर्ष पूर्व एक पूर्ण और विस्तृत इस्लामी इतिहास तैयार करने का काम प्रारंभ किया था। अफ़सोस कि समय की कमी के कारण जो एक नौकरीपेशा इनसान के लिए ऐसे कामों के लिए सबसे बड़ी समस्या है— यह इतिहास अभी तक पूर्ण न हो सका। चूँकि किताब के पूर्ण होने में अभी काफ़ी समय की ज़रूरत है इसलिए यह उचित समझा गया कि फिलहाल उपरोक्त उसूलों का ख़याल रखते हुए एक संक्षिप्त इतिहास तैयार कर दिया जाए जो विद्यार्थियों, कम पढ़े-लिखे लोगों और उन लोगों की ज़रूरत पूरी कर सके जो समय की कमी के कारण विस्तृत इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। प्रस्तुत पुस्तक मेरे इसी प्रयास का नतीजा है। किताब को जनसाधारण के लिए लाभकर बनाने के कारण इसमें न तो अधिक गंभीर विषय आ सकते थे और न इनपर बौद्धिक रूप में बहस की जा सकती थी। बहरहाल किताब की जनसाधारण को आसानी से समझ में आनेवाली हैसियत को बरक़रार रखते हुए जिस हद तक बहस और चिन्तन की गुंजाइश थी, उससे काम लिया गया है। इस उद्देश्य में कहाँ तक कामयाबी हुई है यह फ़ैसला करना पढ़नेवालों का काम है। मैं अपनी सफ़ाई में केवल इतना कह सकता हूँ कि यह अपने अंदाज़ की पहली कोशिश है इसलिए त्रुटियों एवं ग़लतियों की संभावना अधिक है। यदि किसी विद्वान व्यक्ति ने हमारा मार्गदर्शन किया तो न केवल यह कि आगामी संस्करण को बेहतर बनाया जा सकेगा बल्कि इस्लामी इतिहास अध्ययन एवं समालोचना के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और मुझसे अधिक ज्ञान रखनेवाले लेखक अपने अन्वेषण के नतीजों को अधिक पूर्ण और सुन्दर रूप में पेश कर सकेंगे।
प्रस्तुत पुस्तक में हालाँकि चौदह सौ साल के इतिहास को लगभग पाँच सौ पृष्ठों में समेटने की कोशिश की गई है, परन्तु इसका ध्यान रखा गया है कि इस्लामी इतिहास का कोई पहलू चूक न जाए। इस संक्षिप्त पुस्तक में इस्लाम के प्रारंभ से वर्तमान काल तक हर उस क्षेत्र का इतिहास आ गया है जहाँ मुसलमानों ने कभी उल्लेखनीय काम अंजान दिया था। अतः रूस और इण्डोनेशिया जैसे दूर-दराज़ देशों और विशाल रेगिस्तान के दक्षिण में अफ़्रीक़ा के काले बाशिन्दों को भी नज़रंदाज़ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त किताब में केवल विजयों और राजनैतिक मामलों ही का उल्लेख नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बौद्धिक, साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी पेश किए गए हैं। बादशाहों और वज़ीरों के अलावा विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और पर्यटकों के हालात और कारनामे भी अधिक से अधिक बयान करने की कोशिश की गई है। इस्लामी इतिहास पर अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में विभिन्न किताबें लिखी जा चुकी हैं परन्तु इसके बावजूद पढ़नेवाले इस संक्षिप्त एवं आसानी से समझ में आनेवाले इतिहास में एक नई बात पाएँगे और यह महसूस करेंगे कि इतिहास की यह किताब इस्लामी इतिहास के क्षेत्र में एक लाभकारी योगदान है।
किताब के इस परिचय के बाद कुछ वाक्य इस किताब की लेखन-शैली के सम्बन्ध में भी ज़रूरी मालूम होते हैं। इस किताब में पढ़नेवाले को सीधे सम्बोधित किया गया है और प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया गया है कि इस्लामी इतिहास हमारा अपना इतिहास है और विगत चौदह सौ साल में जो भी अच्छे और बुरे काम अंजाम दिए गए हैं वह हमारे ही पूर्वजों के हैं। यदि अच्छे कारनामे हमारे लिए गर्व करने योग्य हैं तो बुरे कामों की शरमिन्दगी भी हमारे ही हिस्से में आएगी। हमें अच्छे कामों को अपना पथ-प्रदर्शक बनाना है और बुरे कामों एवं ग़लतियों से सबक़ हासिल करना है ताकि भविष्य में इन ग़लतियों की पुनरावृति न हो सके।
किताब का उद्देश्य चूँकि अपने इतिहास की रौशनी में भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना है इसलिए मेरे विचार से यह लेखन-शैली इस किताब के लिए समुचित है। यदि किताब ने पढ़नेवालों में वही जज़्बा पैदा कर दिया जो इसका मक़सद है तो समझूँगा कि मेरी मेहनत काम आई। परन्तु यदि किताब इस मक़सद में नाकाम रही तो ख़ुदा से नीयत की शुद्धता का बदला पाने की उम्मीद के अलावा और क्या कर सकता हूँ।
अन्त में अपने प्रिय मित्र महबूबुलहक़ साहब 'वफ़ा' अमतहवी और अपने एक पूर्व सहकर्मी सैयद हबीब अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। इन दोनों दोस्तों ने विशेष कर महबूब साहब ने इस किताब की पाण्डुलिपि को जिस निष्ठा एवं मेहनत से टाइप किया उसके एहसान का मैं बदला नहीं चुका सकता। यदि वे मदद न करते तो किताब के प्रकाशन में मालूम नहीं और कितना विलम्ब हो जाता।
-सरवत सौलत
5 अप्रैल, 1964 ई०
अध्याय-1
ख़ुदा का पैग़ाम
हमारी यह दुनिया कब और कैसे पैदा हुई, इनसान किस तरह वुजूद में आया, यह कायनात (ब्रह्माण्ड) ख़ुद-बख़ुद पैदा हो गई या इसका कोई पैदा करनेवाला भी है, यह दुनिया हमेशा क़ायम रहेगी या किसी दिन दुनिया और उसकी हर चीज़ नष्ट हो जाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जो इनसान के ज़ेहन में पैदा हुए हैं और पैदा होते रहेंगे। परन्तु यह एक ऐसी विकट समस्या है जिसका हल बुद्धि और ज्ञान की मदद से अभी तक नहीं हो सका है। और इसका हल हो भी कैसे सकता है जबकि यह दुनिया उस समय भी मौजूद थी जब इनसान का वुजूद नहीं था, और जब इनसान पैदा हुआ तो वह हज़ारों साल तक लिखने-पढ़ने के क़ाबिल न हो सका। शुरू में उसकी सभ्यता इतनी अविकसित थी कि शहर तो बड़ी चीज़ है, वह गाँव में भी रहना नहीं जानता था। न खेती-बाड़ी कर सकता था और न कोई चीज़ बना सकता था। जंगलों में नंगा फिरता और मकानों की जगह पर गुफाओं में रहता था। पेट भरने के लिए जंगल के फल और पत्तों पर गुज़र करता था। ऐसी स्थिति में इनसान के लिए अपने वुजूद से पहले का हाल बताना तो बड़ी बात है, ख़ुद अपने ज़माने के शुरू के हालात और इतिहास को भी याद रखना मुमकिन नहीं। इसलिए इस दुनिया के जन्म के बारे में कुछ बताना और एक ऐसे दौर के हालात मालूम करना, जब मानव जाति ने इस धरती पर क़दम रखा, नामुमकिन सा है। विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इस बारे में कुछ खोज ज़रूर की है, परन्तु यह यक़ीनी नहीं है और हक़ीक़त से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी प्रकार ग़ैब (परोक्ष) के हालात, यानी ऐसी दुनिया के हालात बताना जिसको हम आँखों से न देख सकते हों, सिर्फ़ अक़्ल के बल पर मुमकिन नहीं है।
जगत का पैदा करनेवाला अल्लाह है
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस दुनिया का कोई पैदा करनेवाला नहीं और यह सब कुछ ख़ुद-बख़ुद पैदा हो गया है। यह बात बुद्धिविवेक से परे तो है ही दिल भी इससे संतुष्ट नहीं होता और यह यक़ीनी तो किसी हाल में नहीं हो सकती। एक तुर्क शायर ने कहा है—
"जब तुम एक किताब पढ़ते हो तो जानते हो कि इसका कोई लिखनेवाला भी है।
और जब तुम एक आलीशान इमारत को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान उसके बनानेवाले की ओर जाता है।
तो क्या ज़मीन और आसमान का कोई बनानेवाला नहीं?
ऐ लोगो! ग़ौर करो और जान लो कि कायनात का यह वुजूद ख़ुद ही इस बात का सबूत है कि उसका पैदा करनेवाला भी कोई है, और वह अल्लाह ही है।"
इस प्रकार सच्ची और दिल को लगनेवाली बात यही है कि कायनात (universe) ख़ुद-बख़ुद पैदा नहीं हुई, बल्कि इसका पैदा करनेवाला भी है। कायनात (सृष्टि) के इसी पैदा करनेवाले को 'अल्लाह' कहा जाता है।
अब यदि अल्लाह ख़ुद अपने बंदों को दुनिया, इनसान और कायनात से सम्बन्धित कोई ख़बर दे तो उसमें कोई शक व शुबहा नहीं होगा।
ख़ुशक़िस्मती से मुसलमानों के पास एक ऐसी किताब है जो इनसान की लिखी हुई नहीं बल्कि वह अल्लाह का कलाम (ईश-वाणी) है। यह 'क़ुरआन' है। हम यहाँ इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि क़ुरआन को अल्लाह की किताब क्यों समझा जाए। अगले पन्नों में संक्षेप में इस विषय पर बहस की गई है। इस विषय पर अलग से बहुत-सी किताबें भी मौजूद हैं।
क़ुरआन के मुताबिक़ दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह की पैदा की हुई हैं। केवल अल्लाह ही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, बाक़ी हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। अल्लाह ने अपने बन्दों के मार्गदर्शन के लिए और ग़ैब की उन बातों को बताने के लिए, जिन्हें कोई व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि की मदद से जान नहीं सकता, एक किताब दी है जिसे 'क़ुरआन मजीद' कहा जाता है। इस किताब में अल्लाह ने दुनिया के प्रारंभ और उसके अन्त से सम्बन्धित कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो किसी और ज़रिया से मालूम नहीं हो सकतीं। चूँकि ये बातें एक ऐसी हस्ती की बताई हुई हैं जो हर चीज़ का पैदा करनेवाला है, इसलिए हमारे लिए मालूमात हासिल करने का इससे ज़्यादा सही और कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह ने अपनी किताब में यह तो नहीं बताया कि इनसान कब पैदा हुआ, हाँ यह ज़रूर बताया कि तमाम इनसान हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) और उनकी बीवी हज़रत हव्वा (अलैहस्सलाम) की औलाद हैं, जो पहले इनसान हैं। क़ुरआन में यह भी बताया गया है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो उनसे यह वादा भी किया था कि आनेवाली नस्लों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह अपने रसूल और नबी (संदेशवाहक) भेजता रहेगा। जो लोग उन रसूलों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे वे कामयाब होंगे। उनकी दुनिया भी अच्छी गुज़रेगी और मरने के बाद आख़िरत (परलोक) की ज़िन्दगी भी अच्छी होगी। परन्तु जो लोग अल्लाह के भेजे हुए उन रसूलों की हिदायत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो उनकी दुनिया तो भले ही अच्छी हो जाए, लेकिन आख़िरत, जो हमेशा की ज़िन्दगी है, अच्छी नहीं होगी।
तौहीद (एकेश्वरवाद) इनसान का पहला अक़ीदा
क़ुरआन के मुताबिक़ इस दुनिया में इनसान इस ज्ञान के साथ आया कि इस कायनात का पैदा करनेवाला सिर्फ़ एक अल्लाह है और इनसान एवं हर जानदार उसका बंदा और ग़ुलाम हैं। साथ ही क़ुरआन हमें यह भी बताता है कि सबसे पहले इनसान का सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान ही नहीं था बल्कि वह इनसान ख़ुद अल्लाह का रसूल और नबी भी था। यह बात कई ग़ैर मुस्लिम विचारकों की इस सोच के विपरीत है कि इनसान का प्रारंभ अज्ञानता के अंधकार में हुआ और अल्लाह पर आस्था एवं विभिन्न धर्म बाद की पैदावार हैं। क़ुरआन कहता है कि यह बात सही नहीं है, हक़ीक़त यह है कि तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना इनसान की सबसे पहली आस्था थी और बाद में इनसान गुमराह होकर मूर्ति पूजा, शिर्क और नास्तिकता की ओर चल पड़ा। क़ुरआन के इस दावे की आधुनिक खोजों से भी पुष्टि होती है।
हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) के बाद जब उनकी औलाद बढ़ी और जगह-जगह फैल गई तो अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया। उसने हर मुल्क और हर क़ौम में अपने चुने हुए मार्गदर्शक और संदेशवाहक भेजे, इन्हें ही हम रसूल, नबी, पैग़म्बर अथवा हादी कहकर पुकारते हैं। ये लोगों को एक अल्लाह की ओर बुलाते थे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ अच्छी बातों का हुक्म देते थे। हमें इन रसूलों में से सिर्फ़ कुछ के नाम मालूम हैं, यानी उनके नाम जिनका क़ुरआन में ज़िक्र है। उनके अलावा दुनिया की दूसरी क़ौमों में जिन बुज़ुर्गों को मार्गदर्शक अथवा संदेशवाहक तथा ईश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए अवतार या पैग़म्बर समझा जाता है, मुमकिन है कि वे भी नबी हों, परन्तु हम यक़ीन के साथ नहीं कह सकते कि वे नबी थे या नहीं क्योंकि हमें सही ढंग से इसका ज्ञान नहीं है और दूसरे उनकी शिक्षाएँ भी अपनी असली हालत में उपलब्ध नहीं हैं।
रसूल और उनकी शिक्षाएँ
जिन नबियों का ज़िक्र क़ुरआन में हुआ है उनमें एक हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। वह अब से लगभग चार हज़ार साल पहले इराक़ के शहर 'उर' में पैदा हुए थे। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) जब बड़े हुए तो अल्लाह ने उनको नुबूवत के पद पर आसीन किया। नबी होने के बाद हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने इराक़ और उससे मिले हुए मुल्कों, शाम (सीरिया) और मिस्र में अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाया। उसके बाद वे अरब देश गए जहाँ उन्होंने अपने बेटे इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के साथ मिलकर शहर मक्का में अल्लाह की इबादत (उपासना) के लिए एक घर बनाया जो 'ख़ान-ए-काबा' कहलाता है। यह वही 'ख़ान-ए-काबा' है जिसकी ओर मुँह करके सारी दुनिया के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं।
हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के बाद भी बहुत-से रसूल आए। उनमें हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) बहुत मशहूर हैं। इन नबियों पर भी अल्लाह ने क़ुरआन जैसी किताबें उतारी थीं जो तौरेत, ज़बूर और इंजील कहलाती हैं। तौरेत हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर, ज़बूर हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) पर और इंजील हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) पर उतरी।
दुनिया का नियम है कि कुछ लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं और अच्छे काम करते हैं, और कुछ लोग ग़लत रास्ते को चुनते हैं और बुरे-बुरे काम करते हैं। अतः उन नबियों की हिदायत पर तो लोग उचित मार्ग को अपना लेते थे, लेकिन उनके बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता था लोग असल मार्ग से भटक जाते थे और अपनी ख़्वाहिशों एवं स्वार्थों की पैरवी करने लगते थे। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम), हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की शिक्षाओं को भी लोगों ने आगे चलकर ऐसे ही भुला दिया। लोगों ने एक अल्लाह की इबादत करने के बदले मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया और दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाने लगे। उन्होंने सबसे ग़लत काम यह किया कि अल्लाह की किताबों में भी काट-छाँट और उलट-फेर करने लगे। तौरेत और इंजील के साथ भी यही हुआ। इस प्रकार यह मालूम करना संभव नहीं रहा कि उन रसूलों की असल शिक्षा क्या थी। उन पैग़म्बरों की उम्मतों (अनुयायियों) ने अपने असल धर्म यानी 'इस्लाम' को बिगाड़ कर वे धर्म बनाए जो इस वक़्त विभिन्न नामों से दुनिया में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ईसा (अलैहिस्सलाम) ने जिस धर्म की शिक्षा दी थी वह इस्लाम ही था, परन्तु उनके बाद उनके अनुयायियों ने ख़ुद हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) को पूज्य बना डाला और उनकी दी हुई शिक्षा के साथ कुछ दूसरी बातें मिला-जुलाकर वह धर्म बना डाला जिसका नाम आज 'ईसाइयत' है।
पिछली उम्मतों की इस गुमराही (पथभ्रष्टता) को दूर करने के लिए और अपने पैग़ाम को क़ियामत तक ज़िन्दा रखने के लिए अल्लाह ने अपना आख़िरी नबी दुनिया में भेजा और उसको एक किताब दी जिसे 'क़ुरआन' कहते हैं। इस किताब में अल्लाह ने वादा किया है कि वह क़ुरआन की क़ियामत तक हिफ़ाज़त करेगा और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देगा, ताकि लोग अपने पैदा करनेवाले का हुक्म और उसकी हिदायत हमेशा असल रूप में पा सकें। यह आख़िरी नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं।
क़ुरआन अन्य रसूलों की तसदीक़ (पुष्टि) करता है
कुछ लोग ग़लतफ़हमी के कारण मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस्लाम का संस्थापक कहते हैं। परन्तु यह ग़लत है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तरह दूसरे नबी इस्लाम के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे अल्लाह के रसूल (ईशदूत) थे। उन्होंने अपनी इच्छानुसार कोई धर्म नहीं गढ़ लिया था, बल्कि अल्लाह का पैग़ाम उसके बंदों तक पहुँचाया था। उन सबका पैग़ाम एक ही था यानी इस्लाम। क़ुरआन किसी नबी के पैग़ाम को रद्द नहीं करता और न दूसरे धर्म की किताब को ईश्वरीय किताब मानने से इनकार करता है। वह सिर्फ़ यह कहता है कि पिछले नबियों की शिक्षाएँ बदल डाली गई हैं और उन किताबों में इतना काट-छाँट किया गया है कि नबियों की असल शिक्षाएँ विकृत हो गई हैं। क़ुरआन उन तमाम नबियों और उनकी असल शिक्षाओं की पुष्टि करता है।
आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के बेटे हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) की नस्ल से हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम), हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की शिक्षाओं को फिर से ज़िन्दा किया। गुमराह लोगों ने उनकी शिक्षाओं में जो ग़लत बातें जोड़ दी थीं, उनको दूर किया और अल्लाह का पैग़ाम उसके असल रूप में दुनिया के सामने पेश किया।
अध्याय-2
इस्लाम से पूर्व
इस्लाम के ज़ुहूर (अभ्युदय) से पहले, यानी उस वक़्त से पहले जब आख़िरी नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नुबूवत मिली और उन्होंने लोगों को इस्लाम की ओर बुलाना शुरू किया, दुनिया बहुत तरक़्क़ी कर चुकी थी। अब लोग गुफाओं और जंगलों में नहीं, शहरों में रहते थे, जहाँ बड़े-बड़े मकान होते और हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध होतीं। लोग खेती-बाड़ी करने लगे थे और वे सभी तरह के अनाज जो आज हम खाते हैं, पैदा करना सीख गए थे। उन्हें सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े बनाना आ गया था। लोहे और विभिन्न धातुओं से बर्तन और ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाने लगे थे। समुद्र पर सफ़र करने के लिए छोटी-छोटी नाव और जहाज़ तथा ज़मीन पर सफ़र के लिए ऊँट, घोड़े, हाथी, बैल और दूसरे जानवरों और उनके द्वारा खींची जानेवाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना जानते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनसान ने पढ़ना-लिखना भी सीख लिया था। बड़ी-बड़ी किताबें लिखी जाती थीं। हालाँकि उस ज़माने में छपाई की व्यवस्था नहीं थी और किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, परन्तु फिर भी इतनी अधिक लिखी जाती थीं कि कुछ शहरों में बड़े-बड़े पुस्तकालय स्थापित हो गए थे। कहने का मतलब यह कि इनसान लौह-युग तथा अज्ञानता व पशुता के दौर से निकलकर ज्ञान और सभ्यता के दौर में दाख़िल हो चुका था।
दुनिया के विभिन्न धर्म
परन्तु जो बात ताज्जुब की है वह यह है कि ज्ञान और सभ्यता के विकास के बाद भी इनसान तौहीद (एकेश्वरवाद) की वह शिक्षा भूल गया था जो अल्लाह ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को दी थी। अल्लाह को मानते तो सब थे, लेकिन उन्होंने एक ख़ुदा के बदले बहुत-से ख़ुदा बना लिए थे और पत्थर के बुतों को ख़ुदा जानकर पूजने लगे थे। अरब के पूर्व में इराक़ और ईरान देश थे जहाँ ईरानी आबाद थे। ये ईरानी एक ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें एक ख़ुदा को स्वीकार किया गया था, परन्तु इसके अलावा उन्होंने आग की पूजा भी शुरू कर दी थी। ईरान के पूर्व में भारतवर्ष था, जहाँ के लोग सभ्यता एवं संस्कृति तथा ज्ञान एवं बुद्धि में बहुत आगे थे। वे स्वयं को एक ईश्वरीय धर्म का अनुयायी कहते थे और यह दावा करते थे कि उनकी धार्मिक पुस्तकें जिनको 'वेद' कहा जाता है, ईश-वाणी हैं, परन्तु इसके बाद भी भारतवासियों ने एक अल्लाह को छोड़कर अनगिनत ख़ुदा बना लिए थे। हर शक्तिशाली वस्तु उनके निकट पूजनीय थी।
मध्य एशिया से लेकर प्रशांत महासागर के तट तक जो देश फैले हुए थे, जिनमें चीन और जापान प्रसिद्ध हैं, उनमें बौद्धमत के अनुयायी आबाद थे। यह धर्म भी भारत से ही निकलकर इन देशों में फैला था। बुतपरस्ती से इस धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु इस्लाम के ज़ुहूर (उदय) के वक़्त बौद्धमत के माननेवालों में भी बुतपरस्ती आम हो गई थी और उन्होंने अपने धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को पूजना प्रारंभ कर दिया था।
अरब के उत्तर-पश्चिम में ईसाई धर्म का ज़ोर था। शाम (Syria), मिस्र (Egypt), एशिया-ए-कोचक, हबश और दक्षिण-पश्चिम यूरोप के लोग आम तौर पर ईसाई थे। वे ख़ुद को हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) का अनुयायी कहते थे, लेकिन उनकी बताई हुई तौहीद की शिक्षा को भुलाकर हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) को ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा कहने लगे थे और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) व हज़रत मरियम (अलैहस्सलाम) के बुत और तस्वीरें तक बनाने लगे थे।
ईसाइयों की तरह यहूदी भी ईश्वरीय धर्म के अलमबरदार थे। वे स्वयं को हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का अनुयायी कहते थे, परन्तु उन्होंने भी हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके बाद आनेवाले पैग़म्बरों की शिक्षाओं को या तो भुला दिया था या विकृत कर दिया था। उन्होंने हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) जैसे पैग़म्बर को फाँसी दिलाने का प्रयास किया। इन यहूदियों का कोई देश नहीं था। रोम सागर के चारों ओर के देशों में इनकी बस्तियाँ मौजूद थीं। अरब में भी कई जगह ईसाइयों की तरह यहूदियों की बस्तियाँ भी थीं।
इस्लाम के अभ्युदय (ज़ुहूर) के वक़्त दुनिया की यही स्थिति थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम क़ौमों में हालाँकि बुतपरस्ती आम थी, परन्तु वे एक आख़िरी नबी का इंतिज़ार भी कर रही थीं जो उन्हें निजात दिलाएगा और सही रास्ता दिखाएगा। यहूदियों और ईसाइयों के धर्मग्रन्थों में तो आख़िरी नबी से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ और ख़ुशख़बरियाँ बहुत स्पष्ट हैं परन्तु ईरान के आतिशपरस्तों (आग को पूजने वाले) और भारत के हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों में भी आख़िरी नबी से सम्बन्धित संकेत मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभ में सभी धर्मों का सरचश्मा (उद्गम) एक था।
अरब : प्राचीन सभ्यता का केन्द्र
अरब देश जहाँ आख़िरी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पैदा हुए और जहाँ ख़ुदा के पैग़ाम 'इस्लाम' को फिर से ज़िन्दा किया गया, सभ्यता और विकास की दौड़ में दुनिया के उन देशों से बहुत पीछे था जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। एक ज़माना था जब अरब के प्राचीन बाशिन्दों ने अरब से निकलकर बाबिल (Babylonia), शाम (Syria), और मिस्र (Egypt) में शानदार हुकूमतें की थीं और सभ्यता एवं संस्कृति को तरक़्क़ी दी थी। बाबिल का शहर मशहूर हुक्मराँ हम्मुराबी, जो एक क़ानूनसाज़ की हैसियत से मशहूर है, अरबों के उसी प्राचीन दौर से ताल्लुक़ रखता है। उसी ज़माने में अरबों ने ख़ास अरब में हज़रमौत के इलाक़े में और ख़लीज फ़ारस (Persian Gulf) से क़रीब अरब के पूर्वी समुद्री तट पर एक शानदार तमद्दुन (संस्कृति) की बुनियाद रखी थी। परन्तु अरबों के ये कारनामे पूर्व ऐतिहासिक काल से ताल्लुक़ रखते हैं और आज उनका हाल मालूम करने का एक मात्र ज़रिया उस दौर के पुराने खंडहरों की वह खुदाई है जो आधुनिक दौर में की गई है। अरबों के इतिहास में उन क़ौमों को 'अरब-बाइदह', यानी वह अरब जो नापैद (लुप्त) हो गए हैं, कहा जाता है। आद और समूद की क़ौमें और हज़रत हूद (अलैहिस्सलाम) और हज़रत सालेह (अलैहिस्सलाम) जैसे रसूल भी इसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं।
ज़ुहूरे इस्लाम से क़रीबी ज़माने में यमन में अरबों ने एक शानदार संस्कृति की बुनियाद डाली थी। यह दौर 'सबा' की सल्तनत का था जो 1100 ई० से 1300 ई० पूर्व तक क़ायम रही। उस ज़माने में खेती, व्यापार (तिजारत), उद्योग-धन्धों का विकास हुआ। बाद के ज़माने में यह तहज़ीब भी ख़त्म हो गई, लेकिन इसका इतना असर बाक़ी रहा कि ज़ुहूरे इस्लाम के वक़्त यमन का इलाक़ा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा तरक़्क़ीयाफ़्ता (विकसित) और मुहज़्ज़ब (सभ्य) समझा जाता था। यहाँ के अधिकतर लोग बुतपरस्त थे, लेकिन यहूदी और ईसाई भी काफ़ी तादाद में थे।
अहदे जाहिलियत (अज्ञान-काल)
ज़ुहूरे इस्लाम के वक़्त यमन को छोड़कर बाक़ी अरब 'नीम-वहशत' (अर्ध-पशुता) की हालत में था। कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी जो अमन क़ायम रख सकती। सारा मुल्क क़बीलों में बँटा हुआ था और हर क़बीला अपनी जगह आज़ाद था और मनमानी करता था। ये क़बीले आपस में लड़ते रहते थे। यदि एक क़बीले का आदमी दूसरे क़बीले के किसी आदमी को क़त्ल कर देता था तो बदला लेना ज़रूरी समझा जाता था और उसकी वजह से लड़ाइयों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता था जो वर्षों जारी रहता था और हज़ारों इनसान बदले की इस जंग में मारे जाते थे।
मुल्क में डकैती और रहज़नी (रास्ता चलते लूट-मार) आम थी। लोग उस ज़माने में क़ाफ़िले बनाकर सफ़र किया करते थे। परन्तु एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करना इतना ख़तरनाक होता था कि क़ाफ़िले के क़ाफ़िले लूट लिए जाते थे। जो क़बीले लूट-मार को पेशा बनाए हुए थे वे उसे बड़े गर्व का काम समझते थे। शराब और जुआ उसी प्रकार आम थे जैसे आज पश्चिमी देशों में आम हैं। बस इतना फ़र्क़ था कि पश्चिम के लोग शिक्षित होने के कारण यह काम तरीक़े से करते हैं और अरब के लोग पढ़े-लिखे न होने के कारण बेढंगे तरीक़े से करते थे। किसी आदमी की जान लेना मामूली बात थी। ज़रा-ज़रा-सी बात पर लड़ पड़ते थे और एक-दूसरे को क़त्ल कर देते थे। लड़की का पैदा होना बहुत बुरा समझा जाता था और उसे बेइज़्ज़ती की निशानी समझा जाता था। ऐसे संगदिल लोग भी मौजूद थे जो लड़की को पैदा होते ही ज़मीन में ज़िन्दा दफ़्न कर देते थे और कोई उनसे इस क़त्ल के बारे में पूछनेवाला नहीं था।
अरब में शिक्षा नहीं के बराबर थी। शहर मदीना में यहूदियों और ईसाइयों में तो कुछ पढ़े-लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन मक्का में लिखना-पढ़ना जाननेवाले लोग सतरह से ज़्यादा नहीं थे।
हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) ने मिलकर अरब में उस जगह जिसे बाद में मक्का का नाम दिया, ख़ुदा की इबादत के लिए पहला घर या मस्जिद बनाई थी जिसे 'ख़ान-ए-काबा' कहा जाता है। हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) उसके बाद मक्का ही में आबाद हो गए। जब 'ख़ान-ए-काबा' बना था तो उस जगह कोई आबादी नहीं थी, लेकिन काबा बनने के बाद उसके चारों ओर लोग आबाद होते चले गए और इस प्रकार एक शहर वुजूद में आ गया जिसे लोग मक्का कहने लगे।
हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया मक्का और अरब के लोग हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) की शिक्षाओं को भूलते चले गए। फिर किसी व्यक्ति ने एक बुत लाकर काबा में रख दिया, जिसे लोग ख़ुदा समझने लगे और इस प्रकार बुतपरस्ती शुरू हो गई और एक वक़्त ऐसा आ गया कि 'ख़ान-ए-काबा' में, जो एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, तीन सौ साठ बुतों की पूजा होने लगी। हर क़बीले ने अपना एक बुत बना लिया था। मक्का में एक अल्लाह को माननेवाले अब भी मौजूद थे, लेकिन ज़ुहूरे इस्लाम (इस्लाम के अभ्युदय) के वक़्त उनकी तादाद अँगुलियों पर गिनी जा सकती थी।
अरबों की कुछ ख़ूबियाँ
इन तमाम ख़राबियों के बावजूद अरबों में कुछ ख़ूबियाँ और विशेषताएँ भी थीं। वे बहादुर थे, निडर थे, दानशील थे, वादे के पक्के थे, आज़ादीपसंद थे और उनकी ज़िंदगी सादा थी। वे दुनिया की अन्य प्राचीन एवं सभ्य क़ौमों की तरह आरामपसंद और ऐशपसंद नहीं थे। उनमें लिखने-पढ़ने का रिवाज नहीं था, परन्तु उनकी ज़बान 'अरबी' दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और मुकम्मल ज़बान थी। इस्लाम के पूर्व की अरबी शायरी आज भी दुनिया की बेहतरीन शायरी में गिनी जाती है। भाषण विद्या यानी तक़रीर में वे किसी को अपना मद्दे-मुक़ाबिल नहीं समझते थे, बल्कि दूसरी क़ौमों को 'अजमी' यानी गूँगा कहते थे। उच्च विचारों को व्यक्त करने और दिलों पर प्रभाव डालने के लिए अरबी से अधिक कोई ज़बान उपयुक्त नहीं थी।
ज़बान की इस ख़ूबी के अलावा भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अन्तर्राष्ट्रीय पैग़ाम के लिए अरब से ज़्यादा उपयुक्त जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती थी। यह मुल्क एशिया और अफ़्रीक़ा के ठीक मध्य में स्थित है और यूरोप यहाँ से बहुत क़रीब है। विशेषकर उस ज़माने में यूरोप की सभ्य क़ौमें ज़्यादातर यूरोप के दक्षिणी हिस्से में आबाद थीं और यह हिस्सा अरब से इतना ही क़रीब है, जितना हिन्दुस्तान और पाकिस्तान।
यह वे हालात थे कि अरब की सरज़मीन पर पैग़म्बरे इस्लाम और आख़िरी नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पैदा हुए। अगले अध्याय में हम दुनिया की उस सबसे बड़ी हस्ती और मानव-जाति के महान उपकारक का हाल बयान करेंगे जिसकी उम्मत (अनुयायी) होने का दावा मुसलमान करते हैं। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी के हालात मालूम करके यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि क़ुरआन का यह दावा कि वह (क़ुरआन) ख़ुदा का कलाम (ईशवाणी) है और नेक लोगों के लिए हिदायत की किताब है, बिलकुल सही और दुरुस्त है।
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का ख़ानदान
हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम)
।
इसमाईल (अलैहिस्सलाम)
।
अदनान (हज़रात इसमाईल की चालीस पीढ़ी के बाद हुए)
।
मअद्द
।
नज़ार
।
मुज़र
।
इलियास
।
मदरका
।
ख़ुज़ैमा
।
कनाना
।
नुज़र
।
मालिक (क़ुरैश)
।
फ़हर
।
ग़ालिब
।
लुवइ
।
काब
।
मुर्रह
।
किलाब
।
क़ुसई
।
अब्दे मनाफ़
।
हाशिम
।
अब्दुल मुत्तलिब
।
अब्बास अब्दुल्लाह अबूतालिब
।
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)
। । । । । ।
क़ासिम इबराहीम ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम फ़ातिमा
अध्याय-3
आख़िरी नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) - 1
मक्का की ज़िन्दगी
हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के तक़रीबन ढाई हज़ार साल बाद 9 रबीउल अव्वल, 53 हिजरी पूर्व (20 अप्रैल 571 ई०) मक्का शहर में पैदा हुए। [आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैदाइश से मुताल्लिक़ मशहूर आम रिवायत 12 रबीउल अव्वल की है। मैंने वह रिवायत ली है जो मौलाना शिबली ने 'सीरतुन-नबी' में और क़ाज़ी सूलैमान मंसूरपुरी ने 'रहमतुल्लिल आलमीन' में लिखी है।] सोमवार का दिन था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) की औलाद में से थे और अरब के मशहूर क़बीले क़ुरैश से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का ताल्लुक़ था।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यतीम पैदा हुए यानी आपके जन्म से पहले ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इन्तिक़ाल हो गया था। जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) छः वर्ष के हुए तो माँ हज़रत आमिना का भी इन्तिक़ाल हो गया। तब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, परन्तु दो साल के बाद वह भी चल बसे। इस प्रकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आठ साल की उम्र ही में बाप, माँ और दादा जैसे प्रिय सम्बन्धियों की मुहब्बत से महरूम (वंचित) हो गए। अन्त में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा अबू तालिब ने आपके लालन-पालन की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्हीं की सरपरस्ती में जवान हुए।
उस ज़माने में अरब में पढ़ने-लिखने का रिवाज नहीं था। अतः आपने भी कुछ नहीं पढ़ा। क़ुरैश का सबसे बड़ा पेशा तिजारत और कारोबार था। इसलिए जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बड़े हुए तो अपने चाचा के साथ तिजारती सफ़रों पर जाने लगे और इस सिलसिले में शाम (सीरिया) और यमन के दूर-दराज़ मुल्कों के चक्कर भी लगाए।
रसूले पाक (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) शुरू ही से हर क़िस्म की बुरी बातों से बचे रहे। न शराब पी और न जुआ खेला। बुतपरस्ती भी नहीं की, जिसका अरब में आम रिवाज था। हमेशा सच बोलते थे, जिसके कारण लोग आपको 'सादिक़' यानी सच्चा आदमी कहकर पुकारते थे। ईमानदारी का यह हाल था कि मक्का के लोग अपने रुपए, पैसे और ज़ेवर आदि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही के पास अमानत के रूप में रखवा देते थे। अमानत रखनेवाले को अरबी में 'अमीन' कहा जाता है, इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का में 'सादिक़' के अलावा 'अमीन' के नाम से भी मशहूर थे।
उस ज़माने में मक्का में एक मालदार औरत थीं जिनका नाम ख़दीजा था। उनके पति का इन्तिक़ाल हो गया था, इसलिए वह अपना तिजारती सामान ईमानदार लोगों के सुपुर्द करके दूसरे मुल्कों को भेजा करती थीं। जब हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ईमानदारी का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने आपको ढेर सारा तिजारत का माल देकर मुल्क शाम की ओर भेजा। जब आप माल बेचकर वापस आए तो हज़रत ख़दीजा पर आपकी ईमानदारी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शादी का पैग़ाम दे दिया। हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बड़ी नेक औरत थीं और अपनी नेकी के कारण ‘ताहिरा' यानी पाक ख़ातून (महिला) कहलाती थीं। आपकी उम्र पच्चीस साल थी और हज़रत ख़दीजा की उम्र चालीस साल यानी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पंद्रह साल अधिक, लेकिन इसके बावजूद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने चचा से मशविरे के बाद हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से शादी कर ली।
नुबूवत की शुरूआत
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह वह ज़माना था जब शहर मक्का और अरब के लोग हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) की शिक्षाओं को भूलकर बुतपरस्ती करने लगे थे और ख़ान-ए-काबा, जो एक ख़ुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, एक ऐसा बुतख़ाना (बुतों का घर) बन गया था जिसमें तीन सौ साठ बुत रखे हुए थे। लोग क़त्ल, लूट-मार, शराबनोशी (मद्यपान), जुआ और भिन्न-भिन्न प्रकार के बुरे कामों में लिप्त थे।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इन तमाम बुराइयों से बचते थे और अपना वक़्त अच्छे कामों में ख़र्च करते थे। जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बड़े हुए तो अपना वक़्त ग़ौर व फ़िक्र, और इबादत करने में गुज़ारने लगे। शादी के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का के क़रीब एक पहाड़ पर चले जाते थे और वहाँ एक ग़ार (गुफा), जिसका नाम 'हिरा' है, में कई-कई दिन रहकर अल्लाह की इबादत करते थे। आख़िर अल्लाह ने एक दिन, जब आप ग़ारे हिरा में इबादत कर रहे थे, अपने फ़तिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) के ज़रिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह का रसूल और नबी होने की ख़ुशख़बरी दी। हज़रत जिब्रील (अलैहिस्सलाम) वही फ़रिश्ते थे जो रसूले पाक (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पहले भी तमाम नबियों को अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाते रहे थे। यह पैग़ाम इस्लाम का पैग़ाम था। यानी अल्लाह को एक मानना और उसके हुक्म के आगे सिर झुका देना, यही इस्लाम का अर्थ है। मुस्लिम या मुसलमान उसे कहते हैं जो ख़ुदा के हुक्म के आगे अपना सिर झुका दे। पैग़म्बरी मिलने के वक़्त आपकी उम्र चालीस साल थी।
जब अल्लाह ने बंदों तक अपना पैग़ाम पहुँचाने के लिए हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को चुन लिया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह पैग़ाम दूसरों तक पहुँचाने का काम तुरंत शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने अपने घरवालों और दोस्तों को इस्लाम का पैग़ाम पहुँचाया। उनसे बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा। आपकी बीबी हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा), चचा के लड़के हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) जिनकी उम्र अभी सिर्फ़ दस साल थी, आपके दोस्त हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और आपके ग़ुलाम हज़रत जै़द (रज़ियल्लाहु अन्हु) को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सच्चाई पर इतना भरोसा था कि तुरन्त इस्लाम क़बूल कर लिया। ये वे हस्तियाँ थीं जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी के ज़ाहिर और बातिन (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जीवन) से भली-भाँति अवगत थे। उन्होंने इस्लाम क़बूल करके यह बात साबित कर दी कि उन्हें प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पैग़ाम की सच्चाई पर पूरा-पूरा यक़ीन था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इसी प्रकार ख़ामोशी से तीन साल तक तबलीग़ (इस्लाम का प्रचार) करते रहे। इस मुद्दत में तक़रीबन चालीस आदमियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया। इस प्रारंभिक दौर में इस्लाम क़बूल करनेवालों में हज़रत उसमान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत तलहा, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत अबू उबैदा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के नाम इस लिहाज़ से नुमायाँ हैं कि बाद के ज़माने में रसूले ख़ुदा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इन साथियों ने, जिनको "सहाबी' कहा जाता है, इस्लामी इतिहास में बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं।
क़ुरैश का विरोध
तीन साल तक ख़ामोशी से इस्लाम की तबलीग़ करने के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ुदा के हुक्म से एलानिया तबलीग़ शुरू कर दी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक दिन मक्का के तमाम लोगों को जमा किया और उनसे पूछा कि तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? सब लोगों ने कहा : आप एक सच्चे आदमी हैं और हमने आपसे कभी झूठी बात नहीं सुनी। आपने कहा, "अगर ऐसा है तो फिर मेरी बात मानो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतपरस्ती छोड़ दो।" लेकिन बुतपरस्ती तो अरबों की घुट्टी में पड़ी थी। उन्हें प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यह बात पसंद न आई। उन्होंने आपको सच्चा मानने के बाद भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बात नहीं मानी और बुतपरस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ़ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही बात कही जो हर क़दामत पसंद (रूढ़िवादी) कहता है कि हम अपने बाप-दादा के तरीक़ों को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इनकार को अरबी में 'कुफ़्र' कहते हैं और इनकार करनेवाले को 'काफ़िर'। इसलिए वे तमाम लोग जो इस्लाम नहीं लाए काफ़िर कहलाए। इस तरह मक्का के लोग दो जमाअतों (ग्रुपों) में बँट गए, जिनमें एक जमाअत मुसलमानों की थी और दूसरी काफ़िरों की।
इसके बाद इस्लाम जैसे-जैसे फैलता गया और मुसलमानों की जमाअत में शामिल होनेवालों की तादाद बढ़ती गई, काफ़िरों (यानी इस्लाम विरोधियों) की परेशानियाँ भी बढ़ती गईं। अब उन्होंने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और मुसलमानों को तरह-तरह से सताना और उनपर ज़ुल्म करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में सारी दुनिया में ग़ुलामी का रिवाज था, यानी तिजारत के सामान की तरह आदमियों को भी ख़रीदा-बेचा जाता था। वे मर्द जिनको ख़रीद लिया जाता था ग़ुलाम और औरतें लौंडी या कनीज़ कहलाती थीं। इस्लाम क़बूल करनेवालों में ग़ुलाम और लौंडियाँ भी थीं। ये ग़ुलाम चूँकि अपने आक़ाओं (मालिकों) के हाथों बेबस होते थे, इसलिए इस्लाम विरोधियों के ज़ुल्म व सितम का सबसे ज़्यादा निशाना यही लौंडी-ग़ुलाम होते थे। इनके आक़ा इन्हें कोड़ों से पीटते, चिलचिलाती धूप में कभी ज़मीन पर और कभी दहकते अंगारों पर लिटा देते, परन्तु इन ग़ुलामों का ईमान इतना पक्का था कि इन्होंने ये सब तकलीफ़ें उठाईं, मगर इस्लाम का दामन हाथ से न छोड़ा। इन साबित क़दम (दृढ़-निश्चयी) और बहादुर ग़ुलामों में हज़रत बिलाल हब्शी (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नाम बहुत मशहूर हैं।
मक्का के इस्लाम विरोधियों का ज़ुल्म बढ़ता गया तो मुसलमानों की एक जमाअत आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हिदायत पर मक्का छोड़कर समुद्र पार एक दूसरे मुल्क में चली गई, जिसे हब्श कहते हैं।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इस्लाम क़बूल करना
इस्लाम का इनकार करनेवालों के ज़ुल्म व ज़्यादतियों के बावजूद इस्लाम का क़ाफ़िला आगे ही बढ़ रहा था और हक़ व सच्चाई की खोज करनेवाले भय एव आतंक के उस वातावरण में भी इस्लाम के दायरे में दाख़िल हो रहे थे।
कठिनाइयों और मुश्किलों के उस दौर में जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस्लाम के दायरे में दाख़िल हो जाता था तो मायूसी में उम्मीद की एक किरण पैदा हो जाती थी। ऐसी ही एक सूरत हब्श की हिजरत के बाद उस वक़्त पेश आई जब मक्का के दो बहादुर और बाअसर आदमी ईमान लाए। उनमें एक हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे और दूसरे हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो उन दस सहाबियों में से हैं जिनको अशरह मुबश्शरह [वे दस सहाबी जिन्हें ज़िन्दगी ही में जन्नत की ख़ुशख़बरी दी गई थी, उनके नाम ये हैं : (i) हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु), (ii) हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु), (iii) हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु), (iv) हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु), (v) हज़रत अबू उबैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु), (vi) हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु), (vii) हज़रत तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु), (viii) हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु), (ix) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और (x) हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बहनोई थे।] कहा जाता है। हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी ताक़त मिली और अब वे खुल्लम-खुल्ला अल्लाह की इबादत करने लगे।
इस बीच मक्का के इस्लाम विरोधियों ने अल्लाह के पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर विभिन्न तरीक़ों से दबाव डालने की कोशिश की। उन्होंने पहले तो हज़रत अबू तालिब से कहकर आपको इस्लाम की तबलीग़ और प्रचार से रोकना चाहा। लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने साफ़ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चाँद भी लाकर रख दिया जाए तो भी मैं इस फ़र्ज़ को अदा करने से नहीं रुकूँगा यहाँ तक कि कामयाब हो जाऊँ या इसी राह में मेरा ख़ात्मा हो जाए।
इसके बाद विरोधियों ने आपको तरह-तरह के लालच देने की कोशिश की। उन्होंने प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा यदि आप शिर्क (बहुदेववाद) और बुतपरस्ती का विरोध छोड़ दें तो हम आपको मक्का का सरदार मान लेंगे। अगर आप किसी मालदार और ख़ूबसूरत औरत से शादी करना चाहें तो हम उससे शादी कर देंगे। इसके अलावा आप दौलत के ख़्वाहिशमंद हैं तो आपको जितनी दौलत की ज़रूरत हो, उसे देने के लिए तैयार हैं।
बनी हाशिम का सामाजिक बायकाट
अल्लाह के आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए, जो एक बड़े मक़सद के लिए काम कर रहे थे, इस क़िस्म के लालच कोई अर्थ न रखते थे। अतः क़ुरैश के सरदार मायूस होकर वापस चले गए। इस मायूसी ने उन्हें और ज़्यादा बेरहम और ज़ालिम बना दिया। अब तक आम मुसलमान इस्लाम विरोधियों के ज़ुल्म के शिकार थे, लेकिन अब उन्होंने ख़ुद प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ज़ुल्म का निशाना बनाना शुरू कर दिया और आख़िरकार उन ज़ालिमों ने एक भयंकर फ़ैसला किया। इस्लाम विरोधियों ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा अबू तालिब से कहा कि वे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क़त्ल करने के लिए उनके सुपुर्द कर दें वरना उनका और उनके ख़ानदान बनू हाशिम का सामाजिक बायकाट कर दिया जाएगा। अबू तालिब हालाँकि इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन वह अपने प्यारे भतीजे को दुश्मनों के सुपुर्द करने के लिए तैयार न हुए। अब उन विरोधियों ने ख़ानदान बनू हाशिम से मिलना-जुलना और हर क़िस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि खाने-पीने की चीज़ें भी उन तक नहीं पहुँच सकती थीं। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और उनके घरवाले मक्का के क़रीब एक पहाड़ी-घाटी में, जो बाद में 'शेअबे अबी तालिब' के नाम से मशहूर हुई, पनाह लेने पर मजबूर हुए। यहाँ खाना न मिलने के कारण या तो फ़ाक़े करने पड़ते या पेड़ों के पत्तों से गुज़ारा करना पड़ता। मुसीबत के ये दिन तक़रीबन तीन साल जारी रहे। आख़िर मक्का के कुछ नेक-दिल लोगों की कोशिशों से यह बायकाट ख़त्म हुआ और प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घरवाले अपने घरों में वापस आए।
मक्का के लोग अब भी प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को तरह-तरह की तक्लीफ़ें देते, गली-कूँचों में आपका मज़ाक उड़ाते और घर के दरवाज़े के सामने काँटे बिछा देते। यह इस्लाम-विरोधी प्यारे नबी को पागल और जादूगर कहते और लोगों को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बातें सुनने से रोकते।
तायफ़ का सफ़र
मक्का के लोगों ने जब अपने रवैए से प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मायूस कर दिया तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का छोड़कर शहर 'तायफ़' चले गए जो मक्का से चालीस मील दूर एक पहाड़ी मक़ाम है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने वहाँ के लोगों को भी समझाने की कोशिश की, परन्तु तायफ़ के लोग मक्कावालों से भी ज़्यादा कठोर साबित हुए। उन्होंने आपका मज़ाक उड़ाया और पत्थर मार-मारकर शहर से निकाल दिया। मजबूरन आपको मक्का वापस आना पड़ा।
मक्का वापस आने के बाद जल्द ही आपके चचा अबू तालिब और आपकी बीवी हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का इन्तिक़ाल हो गया। ये दोनों प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का बहुत बड़ा सहारा थे। उनके इन्तिक़ाल से आपको इतना दुख पहुँचा कि इस्लामी इतिहास में यह साल जिसमें हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) और अबू तालिब का इन्तिक़ाल हुआ, 'आमुल हुज़्न' यानी ग़म का साल कहलाता है।
मदीना में इस्लाम का प्रचार
तायफ़ से वापसी के बाद मुसलमानों के दिन जल्दी ही फिर गए। अल्लाह ने अपने रसूल और उनके साथियों की मेहनत और क़ुरबानियों का बदला देने का फ़ैसला कर लिया। मक्का से साढ़े तीन सौ मील उत्तर में एक शहर है जिसको अब 'मदीना' (Medina) कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में उसे 'यसरिब' कहते थे। यहाँ के लोग आज की तरह उस वक़्त भी नरमदिल और ख़ुश-अख़लाक़ (सदाचारी) थे। उस ज़माने में मदीने में बुतपरस्तों के अलावा यहूदी भी आबाद थे जो अल्लाह और उसके नबियों पर ईमान रखते थे और एक नबी के आने का इन्तिज़ार कर रहे थे। वे मदीना शहर के अरबों से भी इस बात की चर्चा करते रहते थे। मदीना के अरबों को जब ख़बर मिली कि मक्का में एक शख़्स ने नबी होने का दावा किया है तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक वफ़्द (प्रतिनिधि मंडल) हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास मक्का भेजा। उस वफ़्द के लोगों ने जब प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मुलाक़ात की तो उन्हें आपके नबी होने का यक़ीन हो गया और उन्होंने आपस में कहा, "यह वही नबी हैं जिनके बारे में यहूदी भविष्यवाणी करते रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे इस्लाम क़बूल करने के मामले में हमसे बाज़ी ले जाएँ।" इस प्रकार उस वफ़्द के लोगों ने तुरंत इस्लाम क़बूल कर लिया। इसके बाद अगले दो सालों में मदीना से और लोग भी आए और उन्होंने भी इस्लाम क़बूल किया। मदीना के उन मुसलमानों से रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अहद (प्रण) लिया कि वे अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं बनाएँगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िना (व्याभिचार) नहीं करेंगे, अपने बच्चों को क़त्ल नहीं करेंगे, किसी पर झूठे आरोप अथवा लांछन नहीं लगाएँगे और प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की किसी मामले में नाफ़रमानी (अवज्ञा) नहीं करेंगे। मदीना के उन मुसलमानों ने सुलह और जंग दोनों हालतों में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का साथ देने का प्रण (अह्द) किया। इतिहास में इन अह्दों (प्रणों) को 'पहली बैअते अक़बा' और 'दूसरी बैअत अक़बा' के नाम से याद किया जाता है।
इसके बाद मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और इस तरह जो ख़ुशनसीबी मक्का और तायफ़ के लोगों को हासिल न हो सकी वह मदीना के लोगों ने हासिल कर ली। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मदीना के लोगों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए एक सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को मक्का से भेजा जिनकी कोशिशों से शहर के अधिकतर लोगों ने इस्लाम भी क़बूल कर लिया और इस्लामी शिक्षाएँ भी सीख गए।
मदीना में इस्लाम के फैलने के बाद मुसलमानों को एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ मुसलमान इस्लाम विरोधियों के ज़ुल्म से पनाह ले सकते थे और अल्लाह के आदेशों पर आज़ादी से अमल कर सकते थे। मदीना के मुसलमान प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी अपने साथ मदीना ले जाना चाहते थे, लेकिन आपने इस मामले में अल्लाह के हुक्म का इंतिज़ार किया। इस दौरान में मक्का के मुसलमानों को मदीना चले जाने की हिदायत की। अतः मक्का के तक़रीबन तमाम मुसलमान एक-एक करके मदीना चले गए। सिर्फ़ प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दोस्त हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और दो-चार मुसलमान जिनमें आपके चचेरे भाई हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी शामिल थे, मक्का में रह गए।
मदीने की ओर हिजरत (प्रस्थान)
जब तमाम मुसलमान मदीना चले गए तो अल्लाह की तरफ़ से प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी मदीना चले जाने का हुक्म मिला। इस्लाम विरोधियों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आपको जान से मार डालने का फ़ैसला किया और एक रात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घर के दरवाज़े पर तलवारें लेकर जमा हो गए। उनकी योजना थी कि जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सो जाएँगे तो घर में घुसकर आपको क़त्ल कर देंगे। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी, जिनकी उम्र उस वक़्त बाईस साल थी, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ घर ही में थे।
हम पढ़ चुके हैं कि मक्का के लोग अपनी अमानतें प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास रखवाते थे। ये अमानतें उस वक़्त भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास थीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ये अमानतें हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के सुपुर्द करके उनको हिदायत की कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मदीना जाने के बाद वह उनको उनके मालिकों को वापस करके मदीना आ जाएँ। इसके बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपने बिस्तर पर सुला दिया और ख़ुद घर से बाहर निकल गए। बाहर इस्लाम विरोधियों को ऊँघ आ गई थी जिसके कारण उन्हें आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बाहर निकलने की बिलकुल ख़बर नहीं हो सकी। घर से निकलने के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सबसे पहले अपने दोस्त हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घर गए और उन्हें साथ लेकर मदीने की ओर रवाना हो गए। इस्लाम विरोधियों की जब आँख खुली तो वे घर में दाख़िल हुए, लेकिन बिस्तर पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जगह हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को देखकर हैरान रह गए।
मक्का के इस्लाम विरोधियों को अपनी योजना के नाकाम हो जाने का बड़ा अफ़सोस हुआ। उन्होंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पीछा करने की कोशिश की और यह एलान भी कर दिया कि जो शख़्स मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को गिरफ़्तार करके लाएगा उसे सौ ऊँट इनाम दिए जाएँगे। लेकिन उनके दूसरे मंसूबों की तरह यह कोशिश भी नाकाम साबित हुई। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) तीन दिन तक एक ग़ार (गुफा) में, जो ‘गा़रे सौर' कहलाता था और मक्का से सिर्फ़ तीन मील दूर था, छुपे रहने के बाद मदीने की ओर रवाना हुए।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मक्का से रवाना होने की ख़बर मदीना के लोगों को पहले ही मिल गई थी, इसलिए वे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का बड़ी बेचैनी से इंतिज़ार कर रहे थे। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कई दिन के सफ़र के बाद जब मदीना पहुँचे तो लोगों ने शहर से बाहर निकलकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। माहौल ‘अल्लाहु अकबर' के नारों से गूंज उठा। औरतें आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को देखने के लिए घरों की छतों पर पहुँच गईं और छोटी बच्चियों ने गीत गा-गाकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का स्वागत किया। बाद में हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी मदीना पहुँच गए। मदीना जो अब तक 'यसरिब' कहलाता था, प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आ जाने के बाद उसका नाम 'मदीनतुन्नबी' यानी 'नबी का शहर' हो गया। मदीना शब्द इसी 'मदीनतुन्नबी' का संक्षिप्त रूप है।
अध्याय-4
आख़िर नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) - 2
मदीना की ज़िंदगी
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और मुसलमानों के मक्का छोड़कर मदीना चले जाने की घटना को 'हिजरत' कहा जाता है। यह हिजरत इस्लामी इतिहास की एक अहम घटना और एक अहम मोड़ है। अब मुसलमानों को मदीना में एक पनाहगाह मिल गई और उनके मज़लूमियत, मुसीबत और बेबसी के दिन ख़त्म हो गए। अब मुसलमान आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत कर सकते थे और उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक़ अपनी ज़िंदगी को ढाल सकते थे। वे मुसलमान जो इससे पहले हिजरत करके हबश चले गए थे, अब वे भी मदीना आ गए। मदीना अब 'दारुल इस्लाम' (इस्लाम का घर) बन चुका था।
मसजिदे नबवी की तामीर
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मदीना पहुँचने के बाद सबसे पहले दो अहम काम किए। पहले एक मसजिद की बुनियाद डाली गई। यह मसजिद, जो आज दुनिया की अज़ीमुश्शान इबादतगाहों में शुमार होती है, उस समय लकड़ी और फूस आदि की बनी हुई एक इमारत थी जिसका फ़र्श भी पक्का नहीं था। शहर की तरह यह मसजिद भी आख़िरी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की निसबत से मसजिदे नबवी कहलाती है। यह मसजिद सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं थी, बल्कि मदीने की शहरी ज़िंदगी (सामुदायिक जीवन) का एक अहम मरकज़ (केन्द्र) थी। यहाँ मुसलमानों को इस्लामी शिक्षाएँ दी जाती थीं, प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नागरिकों के आपस के झगड़े सुलझाते थे और मुसलमानों पर प्रभाव डालनेवाले मामलों में उनसे सलाह-मशविरा करते थे। नमाज़ के लिए बुलाने के लिए 'अज़ान' देने का तरीक़ा भी इसी ज़माने में शुरू हुआ और यह काम हज़रत बिलाल हब्शी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के सुपुर्द किया गया, जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी थीं। उनकी आवाज़ इतनी मनमोहक और दिलकश थी कि जब वह अज़ान देते थे तो लोग सुनने के लिए खड़े हो जाते थे।
भाईचारे की व्यवस्था
दूसरा अहम काम जो मदीना पहुँचकर किया गया वह 'उख़ूवत' यानी भाईचारे की व्यवस्था थी। मक्का छोड़कर जो मुसलमान मदीना आए उन्हें 'मुहाजिर' का नाम दिया गया, यानी वे लोग जिन्होंने हिजरत की। उसी तरह मदीना के मुसलमानों को 'अनसार' का नाम दिया गया, यानी वे लोग जिन्होंने मदद की। मुहाजिर चूँकि इस्लाम-विरोधियों से छुपकर निकले थे, इसलिए अपने साथ कुछ न ला सके थे। अपना घर और उसकी हर चीज़ मक्का में ही छोड़ आए थे। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हर मुहाजिर को एक अनसारी के सुपुर्द कर दिया और कहा कि यह तुम्हारा भाई है। अनसार ने भी उन्हें अपने सगे भाइयों की तरह समझा और अपनी जायदाद तक में उनको शरीक कर लिया। भाईचारे की यह व्यवस्था एक इंक़लाबी (क्रांतिकारी) क़दम था। क़बायली पक्षपात और द्वेष के उस दौर में जब कि एक क़बीला दूसरे क़बीले को किसी प्रकार की रिआयत देने को तैयार नहीं था, भाईचारे की इस व्यवस्था ने न सिर्फ़ मक्का और मदीना के लोगों को आपस में मिला दिया था, बल्कि उजड़े हुए लोगों का मसला भी हल कर दिया था।
मदीना पहुँचने के बाद प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीसरा अहम क़दम यह उठाया कि मदीना के मुसलमानों, यहूदियों और मुशरिकों (बहुदेववादियों) पर सम्मिलित एक राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद डाली जिसे हम मदीना की शहरी हुकूमत या राज्य कह सकते हैं। इस मक़सद के लिए एक लिखित समझौता भी किया गया, जिसे दुनिया का पहला लिखित संविधान कहा जाता है। इस समझौते या संविधान के तहत यहूदियों और मदीना के मुशरिकों के साथ राजनीतिक एकता क़ायम किया गया जिसमें बालादस्ती इस्लाम और मुसलमानों को हासिल थी। आज की परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि मदीने के इस्लामी राज्य में ग़ैर मुस्लिमों को अन्दरूनी ख़ुदमुख़्तारी (Sovereignty) हासिल थी।
मदीना में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ये कामयाबियाँ और इस्लाम की मज़बूती मक्का के इस्लाम विरोधियों को सख़्त नापसन्द हुई और उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए मुसलमानों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इस उद्देश्य से उन्होंने मदीने पर तीन बार चढ़ाई की, लेकिन तादाद में अधिक होने के बावजूद हर बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी।
मदीना पर क़ुरैश के हमले
इन लड़ाइयों में पहली लड़ाई 'ग़ज़्व-ए-बद्र' कहलाती है, क्योंकि यह जंग मदीना से सत्तर-अस्सी मील दूर बद्र के मक़ाम पर हुई थी। इस जंग में मात्र तीन सौ तेरह मुसलमानों ने एक हज़ार एक सौ दुश्मनों को पराजित किया। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और इस्लाम विरोधियों का सरदार अबू जहल इस जंग में मारा गया।
दूसरी लड़ाई 'ग़ज़्व-ए-उहुद' कहलाती है। इसमें सात सौ मुसलमानों ने तीन हज़ार दुश्मनों का मुक़ाबला किया। इस बार दुश्मनों का सरदार अबू सुफ़ियान था। इस जंग में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) शहीद हो गए और प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी ज़ख़्म आए। परन्तु दुश्मन मदीना पर हमला करने की हिम्मत न कर सके और वापस चले गए। उहुद मदीना के उत्तर में दो मील दूर एक पहाड़ का नाम है जिसके दामन में यह जंग हुई थी।
तीसरी बड़ी लड़ाई 'ग़ज़्व-ए-ख़ंदक़' या 'ग़ज़्व-ए-अहज़ाब' कहलाती है। इस बार मक्का के इस्लाम- विरोधियों ने अरब के कई क़बीलों की मदद और यहूदियों के सहयोग से मदीने का घेराव कर लिया था, और शहर को बचाने के लिए मुसलमानों ने शहर में दाख़िल होनेवाले रास्तों पर ख़ंदक़ (खाई) खोद ली थी। सुरक्षा के लिए ख़ंदक़ खोदने का तरीक़ा अरबों ने एक ईरानी सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के मशविरे पर पहली बार जंग में अपनाया। इस बार भी दुश्मनों का सरदार अबू सुफ़ियान ही था।
अहज़ाब की लड़ाई के बाद प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज करने का इरादा किया। अरब में पुराने ज़माने से यह परम्परा चली आ रही थी कि हज के ज़माने में लड़ाइयाँ बंद कर दी जाती थीं और अरब के हर इलाक़े के लोग बग़ैर किसी पाबंदी के हज कर सकते थे। लेकिन जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक हज़ार चार सौ मुसलमानों के साथ मक्का की ओर रवाना हुए तो हुदैबिया के मक़ाम पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ख़बर मिली कि इस्लाम विरोधी जंग की तैयारी कर रहे हैं और वे मुसलमानों को मक्का में दाख़िल नहीं होने देंगे। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्कावालों को यक़ीन दिलाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हज करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी ज़िद पर अड़े रहे और मुसलमानों को हज करने नहीं दिया। आख़िरकार मक्का के इस्लाम विरोधियों और मुसलमानों के बीच एक समझौता हो गया जो 'सुलह-हुदैबिया' कहलाता है। इस समझौते के अनुसार ये तय पाया कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएँ और अगले साल हज के लिए आएँ। समझौते की कुछ शर्तें ऐसी भी थीं जो ज़ाहिर में मुसलमानों के लिए हानिकारक थीं, लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने शान्ति व समझौते और उसके दूरगामी परिणाम की ख़ातिर ये शर्तें मंज़ूर कर लीं। समझौता हो जाने के बाद मुसलमान मदीना वापस आ गए।
हज़रत ख़ालिद (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इस्लाम क़बूल करना
हालाँकि सुलह हुदैबिया दबकर की गई थी, लेकिन अल्लाह ने क़ुरआन में उसे फ़तह (जीत) बताया है और नतीजे के लिहाज़ से यह वाक़ई फ़तह साबित हुई। सुलह से पहले मुसलमान इस्लाम विरोधियों से अलग-थलग रहते थे। अब सुलह के बाद दोनों में मेल-जोल शुरू हो गया। मुसलमानों के अख़लाक़ (सदाचार) और नेक अमल (सद्व्यवहार) से प्रभावित होकर इस्लाम विरोधी बड़ी संख्या में मुसलमान होने लगे। अतः अगले दो सालों में जिस तेज़ी से लोग मुसलमान हुए, इतने इससे पहले कभी न हुए थे। इस ज़माने में इस्लाम लानेवालों में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नाम सबसे प्रसिद्ध हैं। ये दोनों बड़े अच्छे सिपहसालार (कमांडर) थे और इन्होंने इस्लाम क़बूल करने के बाद आश्चर्यजनक कारनामे अंजाम दिए और कई जंगें जीतीं।
इस्लाम का पैग़ाम किसी एक क़ौम या इलाक़े के लिए ख़ास नहीं है। यह एक आलमी (विश्व व्यापी) पैग़ाम है और सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए है। जब मदीना और अरब के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम की बुनियादें मज़बूत हो गईं तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ईरान, रूम, मिस्र और हबश के बादशाहों को ख़त लिखे और उन्हें इस्लाम की दावत दी। हबश के बादशाह नज्जाशी ने ख़त मिलते ही इस्लाम क़बूल कर लिया, रोम (Greek) के बादशाह हिरक़्ल और मिस्र के रूमी गवर्नर मक़ूक़िस ने इस्लाम तो क़बूल नहीं किया, लेकिन आपके भेजे हुए नुमाइन्दों (सन्देशवाहकों) के साथ अच्छा व्यवहार किया। कई इतिहासकारों का विचार है कि हिरक़्ल को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नबी होने का यक़ीन हो गया था और वह दिल में तो मुसलमान हो गया था, लेकिन ईसाई आबादी के डर से अपने इस्लाम का एलान न कर सका। इसके विपरीत ईरान का बादशाह ख़ुसरो परवेज़ बड़ा घमण्डी साबित हुआ। उसने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के भेजे हुए ख़त को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब इसकी ख़बर मिली तो फ़रमाया कि ख़ुसरो की सल्तनत भी इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यह भविष्यवाणी किस प्रकार शब्द-शब्द सही साबित हुई।
यहूदियों की साज़िशें
ख़ैबर की फ़तह का वाक़िआ भी सुलह हुदैबिया के बाद पेश आया। हम पढ़ चुके हैं कि इस्लाम से पहले मदीना में मुशरिक अरबों के अलावा यहूदी क़बीले भी आबाद थे। यह यहूदी हालाँकि एक नबी के आने का इंतिज़ार कर रहे थे, लेकिन वे यह उम्मीद करते थे कि आख़िरी नबी यहूदियों में होगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो सिवाय कुछ नेकदिल यहूदियों के बाक़ी ने तमाम निशानियों के बावजूद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नबी मानने से इनकार कर दिया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मदीना पहुँचकर हालाँकि यहूदियों से एक सामझौता कर लिया था और उनको अपना समर्थक बना लिया था, लेकिन मदीना के यहूदी पर्दे के पीछे से इस्लाम को नुक़सान पहुँचाने की कोशिशें करते रहे। उन्होंने मक्का के इस्लाम विरोधियों से साज़-बाज़ की और प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को शहीद करने की कोशिश भी की। समझौते की इस प्रकार ख़िलाफ़वर्ज़ी करने के कारण नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। यहूदियों की एक तादाद को क़त्ल की सज़ा दी गई और बाक़ी को मदीना से निकल जाने की सज़ा दी गई। अब यह यहूदी क़बीले मदीना से तक़रीबन एक सौ मील उत्तर में ख़ैबर मरूद्यानों में आबाद हो गए जहाँ कई यहूदी क़बीले पहले से आबाद थे और उन्होंने बड़े-बड़े क़िले बना रखे थे।
यहूदियों ने मदीना से निकलने के बाद भी मुसलमानों का विरोध नहीं छोड़ा और मक्का के इस्लाम विरोधियों से मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहले की तरह ही साज़िशें करते रहे। अतः ख़ंदक़ की लड़ाई के लिए अरब के इस्लाम विरोधियों को ‘ख़ैबर' के इन्हीं यहूदियों ने तैयार किया था। यहूदियों के इस ख़तरे को दूर करने के लिए सुलह-हुदैबिया के एक साल बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ैबर के यहूदियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उस इलाक़े को मदीना की इस्लामी रियासत में शामिल कर लिया। ख़ैबर की इस लड़ाई में हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यहूदियों के सबसे बड़े बहादुर और सूरमा 'मरहब' को क़त्ल कर एक मज़बूत क़िले को फ़तह करके बड़ा नाम पैदा किया।
फ़तह मक्का
सुलह-हुदैबिया के बाद इन लगातार कामयाबियों के कारण मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई और वे इस क़ाबिल हो गए कि मक्का के इस्लाम विरोधियों से दबने के बजाए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। अतः सुलह-हुदैबिया के दो साल बाद जब मक्का के लोगों ने मुसलमानों से किया हुआ समझौता तोड़ दिया तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दस हज़ार मुसलमानों को लेकर मक्का फ़तह करने के लिए रवाना हो गए। मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में देखकर इस्लाम विरोधियों के होश उड़ गए और उन्होंने बिना मुक़ाबला किए शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। इस प्रकार प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) जिन्हें आठ साल पहले मक्का छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, विजेता के रूप में मक्का में दाख़िल हुए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ान-ए-काबा में दाख़िल होकर उसे बुतों से साफ़ किया और इस प्रकार हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की रिवायत के मुताबिक़ खान-ए-काबा में फिर से एक ख़ुदा की इबादत होने लगी।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते तो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम विरोधियों को उनकी करतूतों की सज़ाएँ दे सकते थे। उन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को और मुसलमानों को तरह-तरह से सताया था। लेकिन रहमते आलम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किसी को कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि आम माफ़ी का एलान कर दिया। यहाँ तक कि उस हब्शी को भी माफ़ कर दिया, जिसने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचा हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) को उहुद की जंग में शहीद कर दिया था और अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफ़ियान और उसकी बीवी हिन्द को भी माफ़ कर दिया। यह हिन्द वही औरत थी जिसने हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की लाश को चीर-फाड़कर उनका कलेजा अपने दान्तों से चबाया था।
मक्का की यह शान्तिपूर्ण जीत न केवल इस्लामी इतिहास बल्कि विश्व इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। इतिहास ने इससे पूर्व किसी ऐसे विजेता को नहीं देखा जो दुश्मनों पर विजय हासिल करने के बाद उन्हें इस प्रकार माफ़ कर दे और उनके किए हुए ज़ुल्म व सितम की सज़ा न दे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस सद्व्यवहार का नतीजा यह हुआ कि क़ुरैश के सरदार अबू सुफ़ियान और उसकी बीवी हिन्द इस्लाम की सच्चाई के आगे सिर झुकाने को मजबूर हो गए और दोनों ने इस्लाम क़बूल कर लिया। हिन्द मुसलमान होने के बाद कहा करती थी कि मुसलमान होने से पहले मुझे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से ज़्यादा किसी से नफ़रत नहीं थी और अब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से ज़्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्का में कुछ दिन ठहरकर ज़रूरी काम निपटाया और फिर मदीना वापस आ गए। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का में स्थाई रूप से नहीं रहे, क्योंकि आप मदीना के अनसार को वचन दे चुके थे कि वह अनसार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
मक्का पर मुसलमानों का क़बज़ा इस्लामी इतिहास में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। अरब के लोग क़ुरैश को इज़्ज़त और सम्मान की नज़र से देखते थे और वे क़ुरैश के इस्लाम-विरोधियों और मुसलमानों की कशमकश का बराबर जायज़ा लेते रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इस जंग में जीत गए और मक्का के क़ुरैश हार गए तो उन्हें इस्लाम की सच्चाई का यक़ीन हो गया। अरब के हर हिस्से से क़बीलों के सरदार और आम जनता मदीना आ-आकर इस्लाम क़बूल करने लगे और सिर्फ़ दो साल में सारा अरब मुसलमान हो गया। 23 साल पहले सारा अरब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दुश्मन था और अब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अरब जैसे बड़े मुल्क के हुक्मराँ थे।
आख़िरी हज
सन् 10 हिजरी/फ़रवरी, 632 ई० में, यानी फ़तह मक्का के दो साल बाद और मदीना आने के दस साल बाद, प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज करने का इरादा किया। मुसलमानों को जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस इरादे का पता चला तो वे अरब के हर हिस्से से मदीना पहुँचने लगे, ताकि ख़ुदा के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ हज करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। अनुमान है कि इस मौक़े पर एक लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने हज किया।
हज के मौक़े पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक तक़रीर की जो 'ख़ुत्ब-ए-हिज्जतुलविदाअ' (यानी आख़िरी हज की तक़रीर) के नाम से मशहूर है। यह तक़रीर (भाषण) मानवाधिकारों के इतिहास में अपना एक ख़ास महत्त्व रखती है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया :
"आज अहदे जाहिलियत (अज्ञान-काल) के तमाम दस्तूर (विधान) और तौर-तरीक़े ख़त्म कर दिए गए। ख़ुदा एक है और तमाम इनसान आदम (अलैहिस्सलाम) की औलाद हैं और वे सब बराबर हैं। अरबी को अजमी (ग़ैर अरबी) पर और अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) नहीं। अगर किसी की बड़ाई है तो नेक काम की वजह से है, तमाम मुसलमान भाई-भाई हैं।"
इस तक़रीर में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इंतिक़ाम (प्रतिशोध) के तरीक़े को, जिसका अज्ञान-काल में आम रिवाज था और जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ख़ानदानों में दुश्मनी चली जाती थी और सूद के कारोबार को सख़्ती से मना किया। औरतों और ग़ुलाम के साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुसलमानों को हिदायत की कि वे अल्लाह की किताब यानी क़ुरआन को मज़बूती से पकड़े रहें ताकि गुमराह न हों।
आख़िर में आपने जमा लोगों को सम्बोधित करके कहा, "तुमसे अल्लाह के यहाँ मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे?"
मुसलमानों ने एक आवाज़ में कहा, "हम कहेंगे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ुदा का पैग़ाम हम तक पहुँचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा किया।"
इसपर प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आसमान की ओर उँगली उठाई और तीन बार फ़रमाया, "ऐ ख़ुदा गवाह रहना, ऐ ख़ुदा गवाह रहना, ऐ ख़ुदा गवाह रहना।"
ठीक उसी वक़्त, जब आप ये शब्द कह रहे थे, यह आयत नाज़िल हुई—
“आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को पसन्द कर लिया।" (क़ुरआन, 5:3)
इंतिक़ाल
इसमें कोई शक नहीं कि प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके थे और इस्लाम का पैग़ाम मुकम्मल हो चुका था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह फ़र्ज़ नासाज़गार हालात (विपरीत परिस्थितियों) में अदा किया और हर प्रकार की मुसीबतों और मुश्किलों का मुक़ाबला किया।
परिणामत: 23 साल पहले जो लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आपकी जान के दुश्मन थे, अब उनके लिए आपकी ज़बान से निकला एक-एक शब्द हुक्म की हैसियत रखता था और हर शख़्स आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर अपनी जान क़ुरबान कर देने के लिए तैयार रहता था। 23 साल पहले अरब एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे रहते थे और हर ओर अशान्ति और लूटमार फैली रहती थी अब वही अरब अपने तमाम झगड़ों को भूलकर आपस में घुल मिल चुके थे। क़त्ल, लूटमार और अशान्ति का अन्त हो चुका था। बुतपरस्ती की जगह तौहीद (एकेश्वरवाद) ने ले ली थी। ख़ानदान व क़बीले पर घमण्ड एवं गर्व, जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद सबका ख़ात्मा हो गया था और इसकी जगह मानव एकता और भाईचारे ने ले ली थी। यह नई 'मिल्लते इस्लामिया' इनसानी भाईचारे का एक मिसाली नमूना थी।
यह एक बहुत बड़ा इंक़लाब था जो अरब की सरज़मीन में आया था। इसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी।
हज के बाद प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना वापस आ गए और लगभग तीन महीने बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इन्तिक़ाल हो गया। मसजिदे नबवी के साथ जिस कमरे में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) रहते थे उसी में दफ़न किए गए। यह हिजरत का ग्यारहवाँ साल था। रबीउल-अव्वल की 12 तारीख़ और दिन सोमवार था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उम्र उस समय 63 साल थी।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का जीवन चरित्र
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 23 साल तक इस्लाम की तबलीग़ की, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। मक्का में आपको क़दम-क़दम पर तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने दृढ़ निश्चय और साबित क़दमी से उन तमाम मुश्किलों का मुक़ाबला किया। अपनी जान ख़तरे में डाल दी, परन्तु असत्य के आगे सिर नहीं झुकाया और अपना पैग़ाम जारी रखा। मदीना पहुँचने के बाद जब मुसीबतों का ज़माना ख़त्म हो गया और वह वक़्त भी आ गया जब आप पूरे अरब के शासक बन गए तो भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी में कोई फ़र्क़ नहीं आया। अब अगर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहते तो एक बादशाह की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मदीना पहुँचकर भी आपने जनता की तरह सादा ज़िंदगी गुज़ारी। न महल बनाया, न नौकर-ग़ुलाम रखे। अन्तिम समय तक आप एक ऐसे मकान में रहते रहे जो एक झोपड़े से ज़्यादा नहीं था। ज़मीन पर ही सो जाते या ऐसी चारपाई पर जिसपर कभी-कभी बिस्तर तक नहीं होता था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सारा समय या तो अल्लाह की इबादत में गुज़रता या लोगों की भलाई के कामों में। दिन में अधिकतर रोज़े से रहते और रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुज़ारते। रात में लगातार अधिक समय तक नमाज़ में खड़े रहने से पाँव तक सूज जाते थे। [कुछ लोग समझते हैं कि प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीने आकर बादशाह हो गए थे और यह काम एक नबी या पैग़म्बर की शान के ख़िलाफ़ है। यही ख़याल उस ज़माने के भी कुछ लोगों को हो गया था। अतः यमन के ईसाई सरदार हातिम ताई (जिसकी दानशीलता और फ़य्याज़ी व सख़ावत के क़िस्से मशहूर हैं) के लड़के अदी का भी यही ख़याल था। लेकिन जब वह अपनी बहन के कहने से प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में मदीना पहुँचे तो आपकी सादगी और अख़लाक़ को देखकर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बेहद प्रभावित हुए और आपको तुरन्त नबी स्वीकार कर लिया। उन्हें यक़ीन हो गया था कि प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हालाँकि अरब के शासक हैं लेकिन आपकी ज़िन्दगी और अख़लाक़ बादशाहों और शासकों जैसा नहीं है बल्कि नबियों और पैग़म्बरों जैसा ही है।]
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी क़ुरआन का अमली नमूना (व्यवहारिक रूप) थी। यही कारण है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए 'उस्व-ए-हसना' यानी ज़िंदगी गुज़ारने का सबसे अच्छा नमूना क़रार दिया है। यही कारण है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी का कोई पहलू भी छुपा हुआ नहीं था। बीवियों तक को हिदायत थी कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़ाहिर (प्रत्यक्ष) और पोशीदा (परोक्ष) हर काम से मुसलमानों को बाख़बर रखें ताकि वे अपनी ज़िंदगी भी इसी के मुताबिक़ ढालने की कोशिश कर सकें। यही वजह है कि अच्छे और सच्चे मुसलमान हर ज़माने और हर दौर में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नक़्शे क़दम पर चलने की कोशिश करते हैं। यह बात विश्व इतिहास में किसी दूसरे इनसान को नसीब नहीं हो सकी। यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जिससे न केवल आपकी महानता और बड़ाई ज़ाहिर होती है, बल्कि इससे आपकी सच्चाई का भी पता चलता है।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कभी किसी को ऐसा काम करने का हुक्म नहीं दिया जिसे आप ख़ुद न करते हों। पहले आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ख़ुद अमल करते थे, फिर दूसरों को अमल करने की हिदायत करते थे। आपके स्वभाव में बेहद रहमदिली (दयालुता) थी। जंगों में हिस्सा लिया, परन्तु अपने हाथ से किसी को क़त्ल न किया। [वे जंगें आज की जंगों की तरह नहीं थीं। तमाम जंगें हक़ की बुनियाद पर लड़ी गईं। जंगों में शरीक होनेवाले तमाम सिपाही निहायत अनुशासित होते थे। औरतों, बच्चों एवं बूढ़ों पर अत्याचार नहीं किया जाता था। -अनुवादक]
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ख़ुशमिज़ाज और हँसमुख थे। कभी किसी पर ग़ुस्सा नहीं होते थे। बच्चों से विशेष रूप से बहुत प्यार करते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने अमीर और ग़रीब सब बराबर थे और एक ग़रीब बुढ़िया की बात भी उसी तवज्जोह और ध्यान से सुनते थे जिस तवज्जोह से बड़े-बड़े सरदारों की बात सुनते थे।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का परिवार
इस्लाम में नेक अमल के लिए दुनिया का त्याग ज़रूरी नहीं है, जैसाकि बौध मत, ईसाइयत और हिन्दू धर्म में है और जिसके कारण रहबानियत (संन्यास) को तरक़्क़ी मिली। एक राहिब (बैरागी) दुनिया की ज़िम्मेदारियों से बचता है और नेकी की तलाश में जंगलों और वीरानों में चला जाता है। शादी करना उसकी दृष्टि में एक पाप होता है क्योंकि यह इच्छाओं की पूजा ही है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस दृष्टिकोण और नीति को ग़लत बताया। आपने बताया कि नेक अमल (सद्कर्म) और दुनिया की ज़िंदगी का एक-दूसरे से निकट सम्बन्ध है। अगर हम दुनिया का काम इस प्रकार करें कि उससे अल्लाह ख़ुश हो तो वह नेकी है और यदि हम यही काम इस प्रकार करें कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो तो वह बदी यानी पाप है। शादी-ब्याह और पारिवारिक जीवन एक स्वस्थ समाज के लिए ज़रूरी है और बीवी एवं बच्चों के अधिकारों को पूरा करना भी नेकी है। अतः आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी ज़िंदगी में कई शादियाँ कीं। जब तक हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ज़िंदा रहीं तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कोई शादी नहीं की। लेकिन उनके इन्तिक़ाल के बाद मदीना में कई शादियाँ कीं, जिनमें हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के अलावा बाक़ी तमाम बेवा (विधवा) औरतें थीं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बीवियों को 'उम्मुहातुल-मोमिनीन' यानी मुसलमानों की माएँ करार दिया गया है। [1. उम्मुहातुल-मोमिनीन के नाम ये हैं : 1. हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा), 2. हज़रत सौदा (रज़ियल्लाहु अन्हा), 3. हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा), 4. हज़रत हफ़्सा (रज़ियल्लाहु अन्हा) हज़रत उमर की बेटी थीं और 45 हि/665 ई. में इनकी मृत्यु हुई। 5. हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) जो फ़क़ीरों और मिसकीनों की मदद करने की वजह से उम्मुल मसाकीन कहलाती हैं। शादी के दो-तीन महीने बाद ही 3 हि./624 ई. में इंतिक़ाल हो गया। 6. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ. 61 हि./680 ई., 7. हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ. 20 हि./640 ई., 8. हज़रत जुवैरिया (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ. 50 हि./670 ई., 9. हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ. 44 हि./664 ई., 10. हज़रत मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ.51 हि/671 ई., और 11. हज़रत सफ़िया (रज़ियल्लाहु अन्हा) मृ. 50 हि./670 ई.] कई ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने इतनी शादियाँ करने पर तरह-तरह की आपत्तियाँ की हैं और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कर्म को (हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं) अय्याशी और नफ़्सपरस्ती बताने की भी गुस्ताख़ी की है। लेकिन वे आपत्तियाँ इन इतिहासकारों की तंगनज़री (सीमित सोच) और बदनीयती (दुर्भावना) को ज़ाहिर करती हैं। वर्तमान काल से पहले एक से ज़्यादा शादी करने को कभी बुरा नहीं समझा गया और इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त दी गई है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस्लाम और मुसलमानों के विभिन्न हितों को ध्यान में रखकर एक से ज़्यादा शादियाँ की थीं। एक इनसान जो दिन में रोज़े रखता हो और रात का अधिकतर हिस्सा इबादत में गुज़ारता हो, जो शराब से परहेज़ करता हो, जिसकी ज़िंदगी में गाने-बजाने और मौज-मस्ती को दख़ल न हो और जिसकी ख़ुराक रूखा-सूखा खाना हो, उसपर अय्याशी का इल्ज़ाम लगाना सत्य का ख़ून करना है।
उम्मुहातुल मोमिनीन में हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को हासिल है। इल्मी हैसियत (ज्ञान की दृष्टि) से उन्हें बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी के हालात और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीसों का बहुत बड़ा हिस्सा हम तक हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के ज़रिए ही पहुँचा है। उनका इन्तिक़ाल 57 हिजरी/677 ई. में हुआ।
इन पाक बीवियों के अलावा एक हज़रत मारिया क़िब्तिया (रज़ियल्लाहु अन्हा) थीं जिन्हें मिस्र के गवर्नर ने बतौर लौंडी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ख़िदमत में भेजा था।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चार बेटियों और दो बेटों के बाप थे। [आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बेटियों के नाम ये हैं: 1. हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) — सबसे बड़ी बेटी थीं। हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी ही में 8 हिजरी/629 ई. में इंतिक़ाल हो गया। उनकी शादी ख़ालाज़ाद भाई (मौसी के बेटे) अबुल आस से हुई थी।
2. हज़रत रुक़ैया (रज़ियल्लाहु अन्हा) – आपका 2 हिजरी/623 ई. में इंतिक़ाल हुआ।
3. हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हा) हज़रत रुक़ैया से छोटी थीं। 9 हिजरी/630 ई. में इंतिक़ाल हुआ।
4. हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) — प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सबसे छोटी बेटी थीं और इनके अलावा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सब बच्चे आपकी ज़िन्दगी ही में चल बसे थे, इसलिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनसे बहुत मुहब्बत करते थे। हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की शादी हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से हुई जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चचाज़ाद भाई थे। प्यारे नबी के छ: माह बाद इनका इंतिकाल हो गया।
हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हा) दोनों की शादी एक के बाद एक हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से हुई थी। हज़रत रुक़ैया (रज़ियल्लाहु अन्हा) की कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) और हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हा) की औलाद हुई पर या तो बचपन में चल बसी या उनकी नस्ल नहीं चली। हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के तीन लड़के और दो लड़कियाँ हुईं। उनमें हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की नस्ल आज तक चली आ रही है।]
चारों लड़कियाँ हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से पैदा हुईं। एक बेटे क़ासिम नुबूवत से पहले पैदा हुए लेकिन बचपन में ही इन्तिक़ाल कर गए। दूसरे बेटे इबराहिम 8 हि०/629 ई० में मारिया क़िब्तिया (रज़ियल्लाहु अन्हा) से पैदा हुए, लेकिन उनका भी सवा दो महीने की उम्र में इंतिक़ाल हो गया।
क़ुरआन मजीद
इस्लामी शिक्षाओं का पहला और सबसे बड़ा सरचश्मा (स्रोत) क़ुरआन मजीद है जो क़ियामत तक मुसलमानों के लिए हिदायत की किताब है। यह अल्लाह का कलाम है जो उसके फ़रिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) के ज़रिए 'वह्य' की शक्ल में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर नाज़िल (अवतरित) हुआ। क़ुरआन का अन्दाज़े-बयान और भाषा-शैली प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तक़रीरों और हदीसों से बिलकुल भिन्न है और यह इस बात का सबूत है कि क़ुरआन प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तक़रीरों और हदीसों से बिलकुल भिन्न है और यह इस बात का भी सबूत है कि क़ुरआन प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपना कलाम नहीं, जैसा कि कुछ और मुस्लिम समझते हैं। क़ुरआन में यह दावा किया गया है कि कोई इनसान एक आयत भी ऐसी नहीं लिख सकता जो क़ुरआन की भाषा-शैली का मुक़ाबला कर सके। क़ुरआन ने यह चुनौती उन अरबों को दी थी जो अपनी ज़बान एवं भाषा के सामने सबको तुच्छ समझते थे लेकिन बड़े से बड़ा भाषाविद् (ज़बानदाँ) भी इस चुनौती को क़बूल नहीं कर सका। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब मक्का के इस्लाम विरोधियों के सामने क़ुरआन की आयत पढ़ते तो ऐसा लगता कि उनपर जादू कर दिया गया हो। वे क़ुरआन की आयतों को जादू समझते थे। आज भी क़ुरआन अरबी जाननेवालों के लिए वही असर रखता है और पढ़ने और सुननेवाले को ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ बुद्धि व विवेक पर विजय प्राप्त करती हुई दिल में उतरती चली जा रही है।
क़ुरआन की पहली आयत ग़ारे हिरा में उतरी थी और आख़िरी 'हिज्जतुलविदा' के बाद। आज क़ुरआन जिस रूप में है, यह ठीक वही रूप है जो प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में था। हालांकि क़ुरआन उस समय किताब के रूप में जमा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सूरतों (क़ुरआन में 114 सूरतें हैं) की तरतीब यही थी जो आज है और अनगिनत मुसलमानों ने प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी ही में पूरे क़ुरआन को हिफ़्ज़ (कंठस्थ) कर लिया था।
क़ुरआन मजीद की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ने अपने ज़िम्में ली है। जिस प्रकार पिछले नबियों की किताबों 'तौरेत', 'ज़बूर' और 'इन्जील' में काट-छाँट की गई और उनकी असल शिक्षा को विकृत किया गया, क़ुरआन में क़ियामत तक ऐसी विकृति नहीं आ सकती। क़ुरआन मजीद का यह एक ऐसा चमत्कार है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क़ुरआन को नाज़िल हुए आज चौदह सौ साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक लफ़्ज़ तो क्या एक हर्फ़ (अक्षर) की भी तबदीली नहीं हुई है।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नतें
इस्लामी शिक्षाओं और विधान का दूसरा स्रोत प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की 'सुन्नत' है। सुन्नत प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हिदायत (निर्देश) और अमल (व्यवहार) को कहते हैं। चूँकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क़ुरआन की शिक्षाओं का मुकम्मल नमूना थे और दूसरों को हिदायत करने से पहले ख़ुद क़ुरआन के आदेशों पर अमल करते थे, इसलिए अल्लाह ने आपके व्यक्तित्व को मुसलमानों के लिए 'उस्व-ए-हसना' यानी सबसे अच्छा नमूना क़रार दिया है। क़ुरआन में जगह-जगह हिदायत की गई है कि वे अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हुक्म मानें और यदि किसी बात पर मतभेद हो तो वे अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के निर्देशों से रहनुमाई हासिल करें।
प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीसों का मुकम्मल संग्रह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी में नहीं हुआ था। इसलिए कि न तो उस ज़माने में किताबें लिखने का रिवाज था और न मुसलमान इसकी ज़रूरत महसूस करते थे, क्योंकि प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमेशा उनके सामने मौजूद रहते थे। इसके बावजूद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी ही में कई सहाबा ने कई संक्षिप्त संग्रह तैयार कर लिए थे। लेकिन चूँकि हदीसें, क़ुरआन के आदेशों को समझने का सबसे प्रमाणिक स्रोत हैं, इसलिए जैसाकि हम आगे पढ़ेंगे, बाद में हदीसों को किताबी शक्ल में संकलित करने की ज़रूरत महसूस की गई और उनके कई प्रमाणिक संग्रह तैयार किए गए।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी की मुख्य घटनाएँ
मक्का की ज़िन्दगी
सन 53 हिजरी पूर्व, 9 रबीउल अव्वल (20 अप्रैल, 571 ई०) को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैदाइश हुई।
सन् 28 हिजरी पूर्व - हज़रत ख़दीजा से शादी।
सन् 1 बेअसत - (नुबूवत का आग़ाज़) या 13 हिजरी पूर्व - 9 रबीउल अव्वल, (12 फ़रवरी 610 ई०) को नुबूवत मिली और फ़ज्र एवं अस्र की नमाज़ फ़र्ज़ हुई।
सन् 1 बेअसत - 18 रमज़ान (17 अगस्त 610 ई०) से क़ुरआन का उतरना शुरू हुआ।
सन् 5 बेअसत - हब्शा की ओर हिजरत।
सन् 6 बेअसत - हज़रत हमज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का क़बूले इस्लाम।
सन् 7 बेअसत - बनी हाशिम का सामाजिक बायकाट और नज़रबन्दी। यह बायकाट एक मुहर्रम को शुरू हुआ और 9 बेअसत के आख़िर या सन् 10 बेअसत के शुरू में ख़त्म हुआ।
सन् 10 बेअसत - तायफ़ का सफ़र, हज़रत अबू तालिब और हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का इन्तिक़ाल। इसी साल 27 रजब को मेराज हुई और पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं।
सन् 12 बेअसत - मदीनावालों से पहली बैअत, माह-ज़िलहिज्जा।
सन् 13 बेअसत - मदीनावालों से दूसरी बैअत, माह-ज़िलहिज्जा।
सन् 14 बेअसत (1 हिजरी/622 ई०) - हिजरत मदीना, 27 सफ़र को मक्का से रवानगी।
एक रबीउल अव्वल, (16 सितम्बर, 622 ई०) को 'ग़ारे सौर' से रवानगी।
8 रबीउल अव्वल, (23 सितम्बर, 622 ई०) को क़ुबा में प्रवेश।
मदीना की ज़िंदगी
सन् 1 हिजरी (622 ई०) रबीउल अव्वल : मस्जिद नबवी की बुनियाद, लिखित समझौता।
सन् 2 हिजरी (623/624 ई०) - अज़ान का आग़ाज। ज़कात का फ़र्ज होना। बैतुल-मक़्दिस की बजाए काबा की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म — 15 शाबान। रोज़ों का फ़र्ज़ होना — एक रमज़ान। जंगे बद्र — 18 रमज़ान।
सन् 3 हिजरी (624 ई०) - जंगे उहुद, 6 शव्वाल। वरासत का क़ानून लागू।
सन् 4 हिजरी (624 ई०) - बनु नज़ीर से झड़प, रबीउल अव्वल। परदा का हुक्म - ज़ीक़ादा। शराब पर पाबंदी।
सन् 5 हिजरी (627 ई०) - कुछ फ़ौजदारी क़ानून लागू और परदा के बारे में अन्य आदेश, जंगे अहज़ाब – शव्वाल या ज़ीक़ादा, बनु क़ुरैज़ा पर विजय - ज़िल-हिज्जा।
सन् 6 हिजरी (628 ई० ) - सुलह हुदैबिया — ज़ीक़ादा। हज़रत ख़ालिद (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इस्लाम लाना।
सन् 7 हिजरी (628 ई०) - बादशाहों के नाम ख़त - एक मुहर्रम। ख़ैबर की जंग – मुहर्रम। निकाह व तलाक़ के तफ़सीली क़ानून। जंगे मौता।
सन् 8 हिजरी (629 ई०) - फ़तह मक्का, 10 रमज़ान को मदीना से रवानगी और 20 रमज़ान को मक्का में दाख़िल। सूद पर पाबंदी, हुनैन व तायफ़ की जंग - शव्वाल।
सन् 9 हिजरी (630 ई०) - तबूक की जंग – रजब। हज का फ़र्ज़ होना।
सन् 10 हिजरी (631 ई०) - 9 ज़िलहिज्जा को 'हिज्जतुलविदाअ की तक़रीर'।
सन् 11 हिजरी (632 ई०) - बीमारी और मौत का आग़ाज़ - माह सफ़र के अन्त में। मसजिद नबवी में आख़िरी नमाज़ बाजमाअत इंतिक़ाल से पाँच दिन पहले अदा की। इंतिक़ाल – 12 रबीउल अव्वल, सोमवार का दिन, चाश्त का वक़्त। तद्फ़ीन - 13 रबीउल अव्वल और 14 रबीउल अव्वल के बीच की रात में।
अध्याय-5
मदीना : रियासत और समाज
मदीना हिजरत के बाद हालाँकि अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम विरोधियों के साथ लड़ाइयों में गुज़रा, लेकिन यह समझना सही नहीं होगा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ये दस साल मात्र जंगों की भेंट चढ़ गए। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने की जंगों की तादाद देखकर आम तौर पर लोग इस ग़लतफ़हमी में पड़ जाते हैं कि इन जंगों में बहुत ख़ून-ख़राबा हुआ होगा। हालाँकि वास्तविकता इसके विपरीत है। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में जितनी जंगें हुईं उनमें दोनों ओर से हलाक होनेवालों की तादाद बारह सौ से ज़्यादा नहीं है। यानी एक साल में औसतन 120 लोग मारे गए। इतने कम जानी नुक़सान के नतीजे में अरब जैसा मुल्क जो क्षेत्रफल में भारत के बराबर है, मुसलमानों को मिल गया। क्या दुनिया में कोई क़ौम इतने कम जानी नुक़सान के बदले इतना बड़ा इनक़िलाब (क्रान्ति) लाई है?
दस साल की इस मुद्दत में जंग के मैदान से दूर मदीना के शान्तिपूर्ण वातावरण में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की रहनुमाई में एक नया समाज वुजूद में आ रहा था जो इनसान और उसकी ज़िन्दगी के सम्बन्ध में एक यथार्थवादी सोच और स्वस्थ कल्पना पर आधारित था। उस कल्पना ने पुराने नज़रियात (दृष्टिकोणों) को बदल डाला और एक नए सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे की बुनियाद डाली।
इस्लाम में कायनात का तसव्वुर (कल्पना)
इनसान और कायनात से मुताल्लिक़ इस्लामी तसव्वुर (कल्पना) की बुनियाद 'तौहीद' के अक़ीदे (आस्था) पर है। अतः इस्लाम के पाँच बुनियादी अक़ीदों में सबसे पहला तौहीद है।
"ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह"
यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं।
यही वह कलिमा है जिसके पढ़ने के बाद एक इनसान इस्लाम में दाख़िल होता है। इस कलिमे में आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि यह कायनात ख़ुद-बख़ुद पैदा नहीं हुई, बल्कि इसका रचयिता अल्लाह है। वह एक है और उसका कोई साझी नहीं। क़ुरआन की एक सूरा में अल्लाह के इस तसव्वुर को बड़े जामे अन्दाज़ में बयान किया गया है
"कहो अल्लाह एक है। वह सबसे बेनियाज़ है और सब उसके मुहताज हैं। न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद, और कोई उसका हमसर (समतुल्य) नहीं।" (क़ुरआन, 112:1-4)
कलिमा का दूसरा हिस्सा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नुबूवत से सम्बन्धित है। अल्लाह तक पहुँचने का सही रास्ता वही है जो अल्लाह के रसूलों ने बताया है। इनसान किसी और ज़रिए से अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। दूसरे तमाम ज़रिए काल्पनिक और अपूर्ण हैं, यक़ीनी नहीं है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं और रसूलों के इस सिलसिले की आख़िरी कड़ी हैं। उनपर नुबूवत का ख़ात्मा हो गया, इसलिए उनकी बताई हुई शरीअ़त रहती दुनिया तक एक मात्र जीवन विधान है और उसमें कोई तबदीली नहीं हो सकती।
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नुबूवत की सच्चाई ख़ुद उनका चरित्र है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी आईना की तरह हमारे सामने मौजूद है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सच्चाई और ईमानदारी आपके दुश्मनों ने भी स्वीकार की है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सारी ज़िन्दगी दुनियावी स्वार्थों से ख़ाली रही है। ऐसा सच्चा और निःस्वार्थ आदमी जब यह दावा करता है कि अल्लाह मौजूद है, मुझसे बात करता है और उसने मुझे नबी बनाया है तो फिर एक ईमानदार इनसान आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस दावे को मानने पर मजबूर हो जाता है। अतः प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी में यही हुआ। लोग आपकी पाक ज़िन्दगी और सच्चाई को देखकर ईमान लाते थे और आज भी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी अनगिनत लोगों के लिए इस्लाम तक पहुँचने और अल्लाह को पहचानने का बड़ा ज़रिया है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़ात अल्लाह के वुजूद की चश्मदीद गवाही है जिसपर एक मुसलमान ईमान लाता है।
इस्लामी तौहीद के अक़ीदे का एक लाज़िमी (अनिवार्य) हिस्सा यह भी है कि अल्लाह की ज़ात इनसान की ज़िन्दगी से बेताल्लुक़ नहीं है। उसने इनसान और कायनात को ख़ास मक़सद और इरादे से पैदा किया है। वह हमारी तक़दीर (भाग्य) का मालिक है और हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेगा। दुनिया और इसकी ज़िन्दगी अस्थायी है, लेकिन इनसान की ज़िन्दगी मरने के बाद ख़त्म नहीं होगी। हम एक बार फिर ज़िंदा होंगे और यह नई ज़िन्दगी उन कर्मों के अनुसार होगी जो हमने अपनी मौजूदा ज़िन्दगी में किए हैं। गोया यह दुनिया आख़िरत की खेती है। हम यहाँ जो बीज बोएँगे आख़िरत में उसी की फ़सल काटेंगे। असल ज़िन्दगी आख़िरत की ज़िन्दगी है। इस्लाम के इन अक़ीदों को इन शब्दों में बयान किया गया है—
"मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर और इस पर कि तक़दीर का अच्छा या बुरा होना अल्लाह की तरफ़ से है और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पर।"
तौहीद का अक़ीदा शिर्क (बहुदेववाद) की ज़िद (विलोम) है और शिर्क इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी गुमराही है, उतनी ही बड़ी गुमराही जितनी बड़ी नास्तिकता व अधर्म है। इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक़ शिर्क सिर्फ़ इबादत और पूजापाठ में अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक करने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के आदेशों को छोड़कर किसी और का आदेश मानना भी एक प्रकार का शिर्क ही है। क़ुरआन में इसका स्पष्टिकरण इस प्रकार किया गया है—
“सत्ता और अधिकार अल्लाह के सिवा किसी का नहीं है। उसका हुक्म है कि ख़ुद उसके सिवा तुम किसी की बन्दगी न करो। यही सीधा, सच्चा दीन है।" (क़ुरआन, 12:40)
"जो लोग अल्लाह के बनाए क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला न करें, वही काफ़िर (विधर्मी) हैं।" (क़ुरआन, 5:44)
इस्लाम के अनुसार सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता सिर्फ़ अल्लाह को हासिल है। इस्लाम में यह मुमकिन नहीं कि इनसान ज़बान से तो अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन ज़िन्दगी के मामलात दूसरों के बनाए हुए क़ानून के मुताबिक़ तय करे।
इस्लाम की बुनियादें
तौहीद के आलावा इस्लाम की अन्य चार बुनियादें इबादत से सम्बन्धित हैं। इनका मक़सद भी इनसान को अल्लाह से क़रीब लाना है और उसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज का सुधार करना है। ये चार बुनियादें निम्न हैं :
1. नमाज़ – जो दिन में पाँच बार पढ़ी जाती है यानी फ़ज्र, ज़ुह्र, अस्र, मग़रिब और इशा।
ये नमाज़ें इसलिए हैं कि जब आदमी दुनिया के कामों में व्यस्त हो तो अल्लाह को न भूल सके और उसके ज़ेहन में यह ख़याल मौजूद रहे कि अल्लाह उसके हर काम को देख रहा है। इस प्रकार एक सच्चा मुसलमान उन लोगों के मुक़ाबले बुराइयों से ज़्यादा बच सकता है जो उठते-बैठते अल्लाह को याद नहीं करते।
2. रोज़ा – रोज़े साल में एक बार रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। इसका मक़सद सब्र व ज़ब्त (संतोष और सहनशीलता) की आदत डालना और व्यक्ति का सुधार करना है। यह एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए रोज़ा रखनेवाला एक महीने तक बुरी बातों से बचने और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की कोशिश करता है। अगर यह कोशिश सच्चाई और ईमानदारी से की जाए तो रोज़ा रखनेवाले की बाक़ी ग्यारह महीने की ज़िन्दगी भी बेहतर हो सकती है।
3. ज़कात – यानी वे लोग जो दौलतमंद हैं, अपनी जमा की गई दौलत का चालीसवाँ हिस्सा हर साल अलग कर दें, ताकि ग़रीब और ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। ज़कात निकालना किसी क़िस्म का एहसान नहीं है, बल्कि दौलतमंदों पर समाज के ग़रीब लोगों का हक़ है। यह कोई दुनियावी टैक्स भी नहीं है, बल्कि एक इबादत है और व्यक्ति के सुधार का ज़रिया भी।
4. हज – यानी जिन लोगों के पास इतनी दौलत हो कि वे मक्का जा सकें, तो उनपर ज़िन्दगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। यह एक ऐसी सामूहिक इबादत है जिसमें दुनिया के हर हिस्से और मुल्क के लोग शामिल होते हैं। रंग व नस्ल का भेद मिट जाता है और एक अन्तर्राष्ट्रीय भावना जन्म लेती है, साथ ही इनसानी भाईचारे को बल मिलता है।
हमने इस्लाम के इन अक़ीदों को इसलिए विस्तार से बयान किया है कि इनको समझे बिना इस्लाम के पैग़ाम को और मदीने के इस्लामी समाज को सही तौर पर नहीं समझा जा सकता और यही वे अक़ीदे हैं जिनकी बुनियाद पर मदीने की इस्लामी हुकूमत का ढाँचा तैयार किया गया।
अल्लाह की हाकमियत (सर्वोच्च सत्ता)
ईसाइयत या दूसरे मज़हब की तरह इस्लाम मात्र पूजापाठ और कुछ नैतिक शिक्षाओं का मज़हब नहीं है। इसके लिए क़ुरआन में "दीन" शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है मुकम्मल तरीक़-ए-ज़िन्दगी (पूर्ण जीवन-विधान) यानी ऐसा तरीक़ा जो ज़िन्दगी के सिर्फ़ एक हिस्से से सम्बन्धित न हो, बल्कि पूरी ज़िन्दगी से सम्बन्धित हो वह ज़िन्दगी की रूह (आत्मा) और उसको हरकत देनेवाली ताक़त हो। अतः इस्लाम एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है। राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक — यानी इनसानी ज़िन्दगी का हर पहलू इस्लामी आदेशों का पाबन्द है। इस्लाम में सियासत और मज़हब में विभेद नहीं। सियासत और मज़हब दोनों इस्लामी आदेशों के अधीन हैं। जब हम शब्द 'इस्लाम' इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ़ पूजापाठ और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित कोई मज़हब नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था और जीवन-सिद्धान्त होता है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसे इन शब्दों में स्पष्ट किया है—
“इस्लाम और हुकूमत दो जुड़वाँ भाई हैं। दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना दुरुस्त नहीं हो सकता। अतः इस्लाम की मिसाल एक इमारत की है और हुकूमत गोया उसका निगहबान (संरक्षक) है। जिस इमारत की बुनियाद न हो वह गिर जाती है और जिसका निगहबान न हो वह लूट लिया जाता है।” —कंज़ुल उम्माल
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में मदीना में जो राजनीतिक व्यवस्था क़ायम की गई, वह बादशाहत नहीं थी और न ही वह अरब की प्राचीन क़बाइली व्यवस्था थी। मदीना की रियासत को अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों का पूरा-पूरा ज्ञान था। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस रियासत के सरबराह (संचालक) थे। वे बादशाह, राष्ट्रपति या अमीर (अध्यक्ष) नहीं कहलाए क्योंकि वे उन सबसे ज़्यादा अज़ीम पद पर आसीन थे। वे नबी थे और उनका हुक्म धर्म कर्तव्य की तरह पूरा किया जाता था। वे हुक्मराँ के अलावा लोगों का सुधार करनेवाले भी थे और उन्हें सही रास्ता बतानेवाले भी। मदीना की इस्लामी रियासत का आज की तरह कोई लिखित विधान नहीं था और न ही वे राजनीतिक परिभाषाएँ उस समय प्रचलित थीं जो आज हैं। लेकिन क़ुरआन के आदेशों, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीसों और उस ज़माने के इतिहास पर नज़र डालने से उस रियासत का जो नक़्शा सामने आता है वह कुछ इस प्रकार है—
मदीना की रियासत एक नज़रियाती (सैद्धान्तिक) और हमागीर (सर्वव्यापी) रियासत थी। इस रियासत में किसी शख़्स या अवाम की हाकमियत (सत्ता) के बजाए अल्लाह की हाकमियत (सत्ता) को स्वीकार किया गया था। एक सर्वव्यापी रियासत की हैसियत से इसके अधिकारों का दायरा ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को घेरता था। राजनीति, अर्थव्यवस्था, नैतिकता, शिक्षा, उद्योग-धन्धे, खेती-बाड़ी और सामाजिक मामले सब इसके दायरे के अन्दर थे।
अल्लाह की हाकमियत का मतलब यह नहीं है कि मदीना की रियासत एक ऐसी मज़हबी रियासत थी, जिसे थियोक्रेसी (Theocracy) कहा जाता है। थियोक्रेसी में तमाम अधिकार धर्म-गुरु वर्ग को हासिल होते हैं और वे अपने बनाए हुए क़ानूनों को ईश्वरीय क़ानून क़रार देते हैं। इस्लाम में किसी मज़हबी पेशवा (धार्मिक गुरु) को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ईश्वरीय आदेश स्पष्ट और बिलकुल साफ़ हैं और उनकी हैसियत बुनियादी उसूलों की है। इनसान को अल्लाह का नायब (प्रतिनिधि) क़रार दिया गया है और मुसलमानों की जमाअत को पूरा हक़ दिया गया है कि वे ईश्वरीय आदेशों (जो क़ुरआन और हदीस की शक्ल में मौजूद हैं) की पाबंदी करते हुए रियासत के तमाम अधिकारों का उपयोग करें। इस लिहाज़ से मदीना की इस्लामी हुकूमत एक प्रकार से जम्हूरी हुकूमत (प्रजातांत्रिक सरकार) थी। इसमें अवाम की मर्ज़ी को भी दख़ल था और वह अवाम की भलाई के लिए काम करने पर भी मजबूर थी। अवाम के इन अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक नबी होने के बावजूद, उनसे मशविरा करते थे और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मशविरे के उसूल को एक इस्लामी रियासत के लिए लाज़िमी शर्त क़रार दिया। मौजूदा पार्लियामेंट और क़ानून बनानेवाली समितियाँ उसी मशविरे का आधुनिक रूप हैं। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) विभिन्न अवसरों पर प्रजा और अमीर (प्रशासक) की ज़िम्मेदारियों और अधिकारों की व्याख्या करते रहते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उन हिदायतों में से एक हिदायत यह थी कि अमीरों (प्रशासकों) की इताअत (आज्ञापालन) सिर्फ़ मारूफ़ (नेक काम) में है, मुन्कर (बुराई के काम) में नहीं। यानी मुसलमान अमीर का आज्ञापालन सिर्फ़ उस वक़्त तक कर सकते हैं जब तक वह इस्लामी आदेशों के मुताबिक़ हुकूमत करे। दूसरी सूरत में उसके आज्ञापालन से इनकार किया जा सकता है।
इनसानी भाईचारा
मदीना की रियासत चूँकि एक नज़रियाती (सैद्धान्तिक) रियासत थी, इसलिए इसकी बुनियाद रंग व नस्ल और राष्ट्रीयता पर नहीं थी। इस्लाम में उन तमाम पक्षपातों को जो इनसान को इनसान से जुदा करें, उनके बीच भेद-भाव पैदा करें और रंग, नस्ल एवं राष्ट्र के नाम पर इनसानों के बीच नफ़रत और दुश्मनी पैदा करें, नापसन्दीदा क़रार दिया गया है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्पष्ट शब्दों में एलान कर दिया था कि अरब, ईरानी, काले और गोरे सब इनसान बराबर हैं। वे एक ही आदम की औलाद हैं जो मिट्टी से बने थे। लिहाज़ा एक इनसान को दूसरे इनसान पर फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) नहीं। यदि किसी को फ़ज़ीलत दी जा सकती है तो वह सिर्फ़ नेक अमल (सद्कर्म) की वजह से।
इनसानी भाईचारे का यह पैग़ाम उस ज़माने में एक इनक़लाबी (क्रांतिकारी) आवाज़ थी, क्योंकि ईरानी ख़ुद को अरबों से और अरब ख़ुद को ईरानियों से बेहतर समझते थे और एक-दूसरे को नफ़रत से देखते थे। उसी प्रकार रूमी और यूरोप की दूसरी क़ौमें ख़ुद को अफ़्रीक़ा के काले लोगों से श्रेष्ठ समझती थीं और काले रंगवाली क़ौमों को नफ़रत की नज़र से देखती थीं। इस्लाम की यह शिक्षा आज भी एक इनक़लाबी शिक्षा है, क्योंकि आधुनिक दौर की जातीयता और राष्ट्रीयता ने इनसानों को टुकड़ों में बाँट दिया है और सत्य एवं असत्य की पहचान ख़त्म करके क़ौमों को जातीयता का शिकार बना दिया है। अरब में अरबों के अलावा ईरानी, रूमी और हब्शी बाशिन्दे भी थे, लेकिन सबके अधिकार समान थे। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हिदायत थी कि "अगर तुमपर हब्शी ग़ुलाम भी हाकिम बना दिया जाए तो उसकी इताअत (आज्ञापालन) करो।"
क़ानून की बरतरी (सर्वोच्चता)
मदीना की रियासत में क़ानून को बरतरी हासिल थी और अदालत के सामने अमीर और ग़रीब, ताक़तवर और कमज़ोर सब बराबर थे। कोई आदमी चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो क़ानून की पकड़ से बच नहीं सकता था। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक मौक़े पर फ़रमाया—
“अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे।"
मदीना की रियासत में क़ानून का बुनियादी स्रोत अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम (आदेश) थे। सारी रियासत में इनसाफ़ के लिए क़ाज़ी (चीफ़ जस्टिस) मुक़र्रर थे जो अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों की रौशनी में फ़ैसले करते थे। अपनी राय सिर्फ़ उस वक़्त इस्तेमाल करते थे जब क़ुरआन व सुन्नत में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता था।
ग़ैर मुस्लिम क़ौमों के लिए मौलिक अधिकारों की कल्पना नई है, लेकिन मुसलमानों के लिए यह कोई नई चीज़ नहीं है। मदीना की इस्लामी रियासत में लोगों को वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो आज मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जान और माल की सुरक्षा, औरतों की इज़्ज़त की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, विकलांगों और कमज़ोरों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और बग़ैर किसी रुकावट के हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार, ये वे चीज़ें हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है और ये सब अधिकार इस्लामी रियासत की प्रजा को प्राप्त थे। ग़ैर मुस्लिमों को भी ये तमाम अधिकार मिले हुए थे।
इनसाफ़ क़ायम करना, ज़ुल्म मिटाना, नेकी को बढ़ावा देना और बुराई को मिटाना रियासत का सबसे बड़ा मक़सद था। इसके तहत क़त्ल बहुत बड़ा जुर्म था। ज़िना (बलात्कार), शराब, जुआ और सूदी कारोबार पर पाबंदी थी। दण्डों और सज़ाओं का मुकम्मल क़ानून लागू था जिसके तहत विभिन्न जुर्मों पर सज़ा दी जाती थी। नमाज़ बाजमाअत का इन्तिज़ाम करना और ज़कात वसूल करना भी रियासत की ज़िम्मेदारी थी।
जिहाद
मदीना की रियासत में साम्राज्य विस्तार, सत्ता प्राप्ति, निजी प्रसिद्धि और जातीयता की बुनियाद पर किसी क़ौम को ग़ुलाम बनाने या उसपर प्रभुत्व हासिल करने के लिए जंग करना एक अपराध था। जंग सिर्फ़ अपनी रक्षा, अत्याचार और शोषण के ख़ात्मे और हक़ का बोलबाला करने के लिए जायज़ थी। जंग के दौरान दरिंदगी और बरबरियत से मना किया गया और जंग से सम्बन्धित मानव जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे क़ानून बनाए गए जो आज के आधुनिक जंगी कानूनों से बेहतर हैं।
मदीना की रियासत प्रजा की आर्थिक सुरक्षा और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदार थी। इस मक़सद के लिए कई सुधार किए गए। ज़कात का निज़ाम क़ायम किया गया। आर्थिक शोषण यानी लूट-खसोट ख़त्म करने और धन के सही वितरण के लिए विभिन्न तरीक़े अपनाए गए। कमाई के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों में फ़र्क़ किया गया। सूदी कारोबार को ख़त्म किया गया, क्योंकि सूदी कारोबार इनसान को लूटने का हर ज़माने में सबसे बड़ा ज़रिया रहा है। विरासत का क़ानून लागू किया गया ताकि आदमी के मरने के बाद उसकी दौलत और जायदाद इनसाफ़ के साथ उसकी औलाद और रिश्तेदारों में बँट जाए। उस ज़माने में दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिर्फ़ बड़ा लड़का बाप की जायदाद का अधिकारी होता था और दूसरी औलाद वंचित रह जाती थी। इस्लाम ने न केवल इस ज़ुल्म को ख़त्म किया, बल्कि विरासत के बँटवारे का एक ऐसा निज़ाम क़ायम किया जिसके तहत जमा की गई दौलत कई हिस्सों में बँटने लगी। मदीना में जुआ और सट्टा पर पाबन्दी थी। जमाख़ोरी, कालाबाज़ारी एवं चोरबाज़ारी पर भी रोक थी।
शिष्टाचार और नैतिकता की निगरानी
आम तौर पर हुकूमतों का अवाम की नैतिकता से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। वे हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुधार करती रहती हैं, लेकिन जनता के नैतिक सुधार की ओर ख़ास ध्यान नहीं देती हैं। परन्तु मदीना की रियासत अवाम के अख़लाक़ (नैतिकता) की निगरानी भी करती थी। वह ऐसा माहौल पैदा करना चाहती थी जिसमें इनसान अपने अख़लाक़ी (नैतिक) फ़राइज़ (कर्तव्यों) को भी पहचाने, झूठ न बोले, किसी पर लांछन न लगाए, चोरी न करे, जुआ न खेले, शराब न पीए, व्यभिचार में लिप्त न हो और हया (लज्जा) एवं शर्म की ज़िंदगी गुज़ारे। हया (लज्जा) को इस्लाम में आधा ईमान कहा गया है। मुस्लिम समाज में ख़ानदान को बुनियादी अहमियत हासिल है, इसलिए हर वह चीज़ जो मियाँ-बीवी के सम्बन्ध को ख़राब करे और ख़ानदानी रिश्तों को कमज़ोर करे, इस्लाम में नापसन्दीदा है। जिन्सी आज़ादी और व्यभिचार इसी लिए बहुत बड़ा जुर्म है। यही कारण है कि मदीना की इस्लामी रियासत में नाचने-गाने पर पाबंदी थी। ये बातें भी शराब ही की तरह इनसान के बुरे जज़्बात को उभारती हैं, और इतिहास यह बताता है कि नाच-गाने का शराब और अय्याशी से गहरा सम्बन्ध रहा है।
मदीना में जानदार की तस्वीरें बनाने पर भी पाबन्दी थी क्योंकि ईसाइयत और बौद्ध मत की तरह यह बुतपरस्ती का ज़रिया बन सकती थी। बौद्ध मत और ईसाइयत का बुतपरस्ती से कोई सम्बन्ध नहीं था, लेनिक चित्रकारी और मूर्ति बनाने की कला ने ही महात्मा बुद्ध और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के बुत बनाने और उन्हें पूजने की प्रेरणा दी।
दास-प्रथा में सुधार
मदीना की इस्लामी रियासत में दास-प्रथा का भी सुधार किया गया। पुराने ज़माने में सारी दुनिया में ग़ुलामी का रिवाज था, यानी दूसरे तिजारती माल की तरह इनसान भी बेचे जाते थे। इस प्रकार जो मर्द ख़रीदे जाते थे वे ग़ुलाम कहलाते थे और जो औरतें ख़रीदी जाती थीं उनको लौंडी कहा जाता था। इन लौंडी-ग़ुलामों पर उनके मालिक बड़ा ज़ुल्म करते थे और उन्हें किसी प्रकार का हक़ न देते थे। इस्लाम में ग़ुलामी को क़ानूनन ख़त्म तो नहीं किया गया, परन्तु इस प्रथा में ऐसे सुधार किए गए कि इस प्रथा की शक्ल ही बदल गई। ग़ुलामों को घर के दूसरे सदस्यों के बराबर दर्जा दिया गया। यह हुक्म दिया गया कि मालिक जो ख़ुद खाए वही ग़ुलाम को खिलाए। जो ख़ुद पहने वही ग़ुलाम को पहनाए। कहने का मतलब यह कि ग़ुलाम को भी परिवार का सदस्य बना दिया गया। ग़ुलाम को ज़ुल्म के ख़िलाफ़ और हक़ मारे जाने की स्थिति में अदालत से इनसाफ़ पाने का हक़ भी दिया गया। इसी प्रकार ग़ुलामों के ख़रीदो-फ़रोख़्त पर भी पाबन्दी लगाई गई। अब ग़ुलाम सिर्फ़ जंगी क़ैदी ही बनाए जा सकते थे। इसके अलावा लौंडी, ग़ुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ा सवाब (पुण्य) बताया गया और इस तरह फ़ितरी तरीक़े से दास-प्रथा का ख़ात्मा हो गया।
औरतों के अधिकार
इस्लाम ने औरतों को वे अधिकार भी दिए जो इससे पहले दुनिया में किसी मुल्क की औरतों को हासिल नहीं थे। पहले बाप या किसी निकट सम्बन्धी की विरासत में लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने विरासत में लड़कियों का हिस्सा मुक़र्रर किया। औरतों को कमाने का हक़ देकर उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता दी। उस ज़माने में औरतें आम तौर पर तुच्छ और अपमानित थीं, लेकिन इस्लाम ने बताया कि एक इनसान की हैसियत से औरत और मर्द दोनों बराबर हैं और उनमें कोई अपमानित और कोई सम्मानित नहीं हो सकता। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बताया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। क़ुरआन ने औरतों को मर्दों का और मर्दों को औरतों का लिबास क़रार दिया है। बहुत-से मुल्कों में विधवा शादी नहीं कर सकती थी, इस्लाम ने विधवाओं को भी शादी का हक़ दिया। कई मुल्कों में औरतों को तलाक़ का हक़ हासिल नहीं था, इस्लाम ने औरतों को भी मर्द से तलाक़ लेने का हक़ दिया।
इन तमाम अधिकारों के साथ इस्लाम में औरतों और मर्दों के लिए कुछ सीमाएँ भी मुक़र्रर की गई हैं। औरतों को घर के कामों का और मर्दों को बाहर के कामों का ज़िम्मेदार क़रार दिया गया है। ख़ानदान का संचालन मर्द के सुपुर्द है। ज़रूरत के तहत औरत और मर्द एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। औरतों को मर्दों की और मर्दों को औरतों की शक्ल बनाने से रोका गया है। मर्दों और औरतों के दरमियान आज़ादाना मेल-जोल पर पाबंदी लगाई गई है, ताकि मुस्लिम समाज में वह बेहयाई और बेशर्मी न फैल सके जो इस्लाम से पहले अरबों, यूनानियों, रूमियों और दूसरी क़ौमों में फैल गई थी और जो आजकल पश्चिमी देशों में फैली हुई है। परदे का वास्तविक उद्देश्य मर्दों और औरतों के इसी आज़ादाना मेलजोल को रोकना है। इस्लाम में शादी के लिए लड़की की सहमति ज़रूरी है। लड़की होनेवाले पति को देख भी सकती है।
नग्नता का व्यभिचार से गहरा ताल्लुक़ है। यह देखा गया है कि एक क़ौम लिबास के मामले में जितनी नग्न होती है उसमें व्यभिचार एवं कुकर्म भी उसी अनुपात में होते हैं। इस्लाम में लिबास के मामले में भी हया और शर्म का एक मेयार है, जिसे 'सतर' कहा जाता है। अतः मदीना की रियासत में मर्दों और औरतों के लिए ऐसा लिबास मुक़र्रर किया गया था जो उस मेयार के मुताबिक़ हो।
उस ज़माने में हर देश के धनी लोग एक वक़्त में कई-कई शादियाँ करते थे और शादी की तादाद पर कोई पाबन्दी नहीं थी। मौजूदा दौर में हालाँकि एक से ज़्यादा शादी नहीं की जाती, लेकिन सेक्स सम्बन्ध पर कोई पाबन्दी नहीं। अतः मौजूदा दौर के धनी लोग आम तौर पर ग़ैर औरतों से नाजायज़ सम्बन्ध रखते हैं। इस्लाम ने इस समस्या को इस प्रकार हल किया है कि नाजायज़ सम्बन्ध को बहुत बड़ा गुनाह क़रार दिया और मर्द की फ़ितरत (प्रकृति) को ध्यान में रखते हुए उसे चार बीवियों की हद तक शादी की इजाज़त दी है, लेकिन बीवियों के दरमियान इनसाफ़ को लाज़िमी (अनिवार्य) क़रार दिया है।
ये वे ज़ाब्ते और क़ानून हैं जिनको मदीने की रियासत में लागू किया गया था और जिन्हें आधुनिक परिभाषा में संवैधानिक नियम कहा जाता है।
अरबों की ज़िंदगी में क्रान्तिकारी परिवर्तन
यह था मदीना का नया समाज और नई सभ्यता। यह आदर्श समाज था जिसकी मिसाल इतिहास में और कहीं नहीं मिलती। यह समाज ज़ुल्म व अत्याचार से पाक था। इसकी बुनियाद किसी से नफ़रत (घृणा) पर नहीं, बल्कि पारस्परिक प्रेम पर थी। इसमें रंग व नस्ल, क़ौम व वतन और आक़ा व ग़ुलाम का विभेद नहीं था। इस दौर के मुसलमानों में वे तमाम नैतिक गुण मौजूद थे, जिन्हें हर दौर और ज़माने में अच्छा समझा गया है। इस दौर के मुसलमान उन तमाम बुराइयों से जिन्हें सब बुरा समझते हैं, इस हद तक दूर थे, जिस हद तक कि एक इनसान के लिए मुमकिन हो सकता है और उन्होंने वे तमाम गुण अपना लिए थे जिन्हें सारी दुनिया अच्छा समझती है। यही कारण है कि प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया—
"सबसे अच्छा ज़माना मेरा है, इसके बाद उन लोगों का जो मेरे बाद आएँगे और फिर उन लोगों का जो उनके बाद आएँगे।"
मदीना में जो सुधार किए गए उनका नतीजा यह निकला कि कुछ ही सालों में अरबों की ज़िंदगी में इनक़िलाब (क्रांतिकारी परिवर्तन) आ गया। चोरी, डकैती ख़त्म हो गई, रास्ते सुरक्षित हो गए। अब अरब के हर हिस्से में मुसाफ़िर अकेला सफ़र कर सकता था और कोई उसे टोक नहीं सकता था। लोगों ने शराब, जुए और बेशर्मी व बेहयाई के कामों से तौबा कर ली। वे अरब जो ज़रा-ज़रा सी बात पर इनसान को क़त्ल कर देते थे, वे अब इनसानी जान का एहतराम करने लगे। झूठ, चुग़ली, धोखा, फ़रेब और वादाख़िलाफ़ी की जगह सच्चाई, वफ़ादारी और नैतिकता ने ले ली। तिजारत और कारोबार से सूदी लेन-देन ख़त्म हो गया।
इस्लाम की ये शिक्षाएँ जिन्हें मदीना में व्यावहारिक रूप दिया गया, वक़्ती नहीं हैं। इनसे हर ज़माने और हर दौर में रहनुमाई (मार्गदर्शन) हासिल की जा सकती है। जिस प्रकार सच्चाई, ईमानदारी, इनसाफ़, निःस्वार्थता, दानशीलता, वीरता और वे तमाम अच्छी बातें जिन्हें आलमगीर सच्चाई कहा जाता है कभी पुरानी नहीं हो सकतीं, उसी प्रकार इस्लामी शिक्षाएँ भी कभी पुरानी नहीं हो सकतीं।
इस्लाम दीने फ़ितरत (प्राकृतिक धर्म) है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो इनसान के फ़ितरी तक़ाज़ों (नैसर्गिक माँगों) के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह का वुजूद एक हक़ीक़त है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यही हाल आख़िरत और उस दिन का है जब बदला दिया जाएगा। इनमें कोई बात इनसान की ज़िंदगी में पुरानी होनेवाली नहीं। इसी प्रकार कारोबार में सूद से बचना, खाने-पीने में हलाल व हराम का फ़र्क़ करना, शराब और जुए से परहेज़ करना, ज़िना (बलात्कार), कुकर्म, अश्लील और गन्दी बातों से बचना, औरतों और मर्दों में अज़ादाना मेल-जोल में एहतियात, इस्लाम में विरासत और ज़कात का निज़ाम और दूसरी नैतिक शिक्षाएँ जिनकी चर्चा की जा चुकी है, हक़ीक़त में आलमगीर सच्चाइयाँ (ब्रह्म-सत्य) हैं, इनमें कोई चीज़ पुरानी होनेवाली नहीं। जो चीज़ें पुरानी होनेवाली हैं, इस्लाम ने उन्हें दीन (इस्लाम) का हिस्सा नहीं बनाया और उनके बारे में इस्लाम के उसूलों को सामने रखकर फ़ैसला करने का अधिकार आम मुसलमानों को दिया है।
इस्लाम में जो पाबंदियाँ मुसलमानों पर लगाई गई हैं उन्हें क़ुरआन में 'हुदूदुल्लाह' कहा गया है और उनका मक़सद सिर्फ़ यह है कि इनसान अपनी इच्छाओं की पैरवी में और अपनी अक़्ल व बुद्धिमानी के घमण्ड में अपनी सीमा से आगे न बढ़ जाए और गुमराह होकर किसी खड्ड में न गिर जाए, बल्कि उस रास्ते पर चले जिसे इस्लाम में 'सिराते मुस्तक़ीम' (सीधा रास्ता) कहा गया है और इनसान के नजात का रास्ता (मुक्तिमार्ग) है। ये पाबन्दियाँ क़ैद नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ सुरक्षा के लिए दीवारें हैं। इन पाबन्दियों के बाद एक मुसलमान पूरी तरह आज़ाद है कि वह अपनी अक़्ल, योग्यता और हिम्मत से काम लेकर जिस तरह चाहे अपनी ज़िन्दगी की तामीर करे। इसकी तरक़्क़ी इनसान की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता पर निर्भर है।
मुसलमानों ने इस्लाम की इन शिक्षाओं पर हर दौर में अमल करने की कोशिश की। इस मक़सद में वे कामयाब भी हुए और नाकाम भी। लेकिन जब भी उन्हें कामयाबी हुई तो उनकी हुकूमत के तहत लोगों को सुख व चैन मिला और जब भी उनकी नाकामी हुई तो दुख और मुसीबत के दरवाज़े खुल गए। हम अगले पृष्ठों में देखेंगे कि इस्लामी इतिहास में मुसलमान जिस हद तक इस्लामी शिक्षाओं पर अमल करने में नाकाम हुए उस हद तक ख़राबियाँ पैदा हुईं और जितना अधिक इन शिक्षाओं पर अमल किया उतना ही अधिक फ़ायदा पहुँचा।
मुसलमानों की इस जिद्दोजुहद की दास्तान अब हम अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे।
अध्याय-6
रूम और ईरान की हुकूमतों का ख़ात्मा
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु)
हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का जब इंतिक़ाल हुआ तो सारा अरब मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ चुका था और मुल्क में एक मरकज़ी हुकूमत (केन्द्रीय सरकार) क़ायम हो गई थी जिसके संचालक ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) थे। हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने चूँकि अपने बाद किसी को जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर नहीं किया था इसलिए अब यह फ़ैसला करना आम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जगह इस्लामी रियासत का संचालक कौन हो। अतः मुसलमानों ने मदीना में एक जगह जमा होकर, जिसे 'सक़ीफ़ा बनी साइदह' कहा जाता है, बहस व मुबाहिसा के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का जानशीन यानी 'ख़लीफ़ा' चुन लिया।
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इस्लामी इतिहास में बहुत बड़ा मरतबा है। वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के गहरे दोस्त थे और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए थे। उन्हें आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बातों की सच्चाई पर इतना यक़ीन था कि वह आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हर दावे और हर बात की बग़ैर किसी शक व शुबहा के तसदीक़ (पुष्टि) कर देते थे। इसी कारण हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) 'सिद्दीक़' के नाम से पुकारे जाते थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हर मुशकिल और हर नाज़ुक मौक़े पर प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का साथ दिया और अपनी दौलत से मुसलमानों की मदद की। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमाया करते थे कि अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के माल ने मुझे जितना फ़ायदा पहुँचाया उतना किसी दूसरे के माल ने नहीं पहुँचाया। इंतिक़ाल से पहले जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बीमारी के कारण मसजिदे नबवी में जाने के क़ाबिल न रहे तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुक्म से हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही मुसलमानों की इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे।
'सक़ीफ़ा बनी साइदह' में ख़लीफ़ा चुने जाने के बाद दूसरे दिन मसजिदे नबवी की आम सभा में हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हाथ पर मुसलमानों ने 'बैअत' ['बैअत' का अर्थ होता है आज्ञापालन का अह्द (प्रण) करना। यह वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक आम मुसलमान अपने चुने हुए ख़लीफ़ा के हाथ में हाथ देकर यह वादा करता है कि वह हमेशा उसका अदेशानुपालन करेगा।] की और इस प्रकार हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों के पहले ख़लीफ़ा हो गए। बैअत के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक तक़रीर की जिसमें उन्होंने जनता के अधिकारों और हुक्मरान (शासक) के कर्त्तव्यों पर रौशनी डालते हुए फ़रमाया—
“लोगो! मैं तुमपर हाकिम बनाया गया हूँ हालाँकि मैं तुम्हारी जमाअत में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी इताअत (आदेशानुपालन) करो और अगर ग़लत रास्ते पर चलूँ तो मुझे सीधा कर दो। तुममें जो कमज़ोर है वह भी मेरे निकट ताक़तवर है, यहाँ तक कि मैं उसका हक़ उसे दिला दूँ। और तुम्हारा ताक़तवर आदमी भी मेरे निकट कमज़ोर है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक़ हासिल कर लूँ। अगर मैं ख़ुदा और उसके रसूल की इताअत करूँ तो मेरी इताअत करो और अगर मैं उसकी नाफ़रमानी करूँ तो तुमपर मेरी इताअत लाज़िम (अनिवार्य) नहीं।”
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की इस तक़रीर में साफ़ तौर पर कहा गया है कि एक मुसलमान हुक्मराँ डिक्टेटर नहीं हो सकता और मनमानी नहीं कर सकता। उसके लिए इस्लामी उसूलों पर चलना ज़रूरी है और यदि वह ऐसा न करे तो अवाम उसको हटा सकती है। उनकी यह तक़रीर इस लिहाज़ से बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें अवाम के अधिकारों की जो निशानदेही की गई है और हुक्मरान के जो कर्त्तव्य और सीमाएँ मुक़र्रर की गई हैं वे इस्लाम की राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी महत्त्व रखती हैं और बाद में अन्य ख़लीफ़ाओं ने भी उनको अपना रहनुमा उसूल बनाया। ये वे अधिकार एवं कर्त्तव्य हैं जिन्हें पश्चिम जगत ने अठारहवीं शताब्दी में अपनाया।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में हालाँकि पूरे अरब पर मुसलमानों की हुकूमत क़ायम हो गई थी, लेकिन तमाम लोग अभी इस्लाम नहीं लाए थे और जो इस्लाम ला चुके थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दिल से इस्लाम क़बूल नहीं किया था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंतिक़ाल के बाद ऐसे ही क़बीले के एक शख़्स मुसैलमा ने तो नबी होने का दावा कर दिया। चूँकि यह शख़्स झूठा था इसलिए इसे 'मुसैलमा कज़्ज़ाब' यानी झूठ बोलनेवाला कहा जाता है—
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सबसे पहले उन बाग़ियों का मुक़ाबला किया। फ़ौजें रवाना कीं और सबको इताअत पर मजबूर कर दिया। इन लड़ाइयों में एक सहाबी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, जो इस्लामी फ़ौज के कमान्डर थे, बड़ा नाम कमाया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी उन्होंने एक सख़्त जंग के बाद हराया।
उस ज़माने में अरब की सरहद पर दो बड़ी हुकूमतें थीं। एक ईरान की हुकूमत और दूसरी रूम की हुकूमत जिसे बाज़नतीनी हुकूमत भी कहते हैं। ईरान का बादशाह 'किसरा' और रूम का बादशाह 'क़ैसर' कहलाता था। हम पढ़ चुके हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन दोनों बादशाहों को इस्लाम क़बूल करने के लिए ख़त लिखे थे। क़ैसरे रूम ने जिसका नाम हिरक़्ल (Heraclius) था इस्लाम तो क़बूल नहीं किया लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के भेजे हुए नुमाइन्दे से अच्छा सुलूक किया। इसके विपरीत ईरान के बादशाह ख़ुसरो परवेज़ ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का ख़त फाड़कर फेंक दिया और मुसलमान नुमाइन्दे को दरबार से निकलवा दिया।
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब इसकी ख़बर मिली तो आपने कहा कि उसकी सल्तनत भी इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) किस प्रकार सच साबित हुई। उस ज़माने के ईरानी जिनका धर्म अग्नि-पूजन था, अरबों से बड़ी नफ़रत करते थे और सरहद पर ईरानियों और अरबों में लड़ाइयाँ होती रहती थीं। जब यह अरब मुसलमान हो गए तो इन लड़ाइयों ने और ज़ोर पकड़ लिया और हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) से सरहद के अरबों ने मदद माँगी। और इस प्रकार आतिशपरस्तों और मुसलमानों में बाक़ायदा जंग शुरू हो गई।
उधर ईरानियों से जंग शुरू हुई तो इधर रूमियों से भी जंग शुरू हो गई। दूसरी वजह यह थी कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने ही में रूमियों और मुसलमानों में झगड़े शुरू हो गए थे। रूम के एक शहर 'बसरा' के हाकिम ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नुमाइन्दे को क़त्ल भी करवा दिया था। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बदला लेने के लिए एक फ़ौज भी भेजी थी, लेकिन वह रूमी लशकर की अधिक तादाद के कारण ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़लीफ़ा होने के बाद शाम (Syria) पर, जो रूमियों के क़ब्ज़े में था, बाक़ायदा फ़ौजी कार्यवाही शुरू कर दी।
लेकिन मुसलमान अपनी सल्तनत के विस्तार के शौक़ीन नहीं थे। वे तो सिर्फ़ यह चाहते थे कि इस्लाम को फैलने में आज़ादी हो, ताकि लोग उसकी शिक्षाओं पर अमल करके बुराइयों से बचें और अच्छे काम करें। इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने ईरानियों और रूमियों दोनों को इस्लाम की दावत दी और कहा कि यदि वे इस्लाम क़बूल कर लें तो लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह स्वीकार न हुआ। अब मुसलमानों ने कहा कि अच्छा अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो हमारी इताअत क़बूल कर लो और इस इताअत के सुबूत में जिज़िया दो। लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार न हुआ। अब मुसलमानों के लिए सिवाए इसके कोई रास्ता न रहा कि वे उनके ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दें। अतः ईरान और रूम की दोनों हुकूमतों से एक ही वक़्त में मुसलमानों की जंग शुरू हो गई। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) को हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने पहले ईरान की ओर भेजा। वहाँ कई शहर फ़तह करने के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हुक्म पर वह रूमियों के मुक़ाबले के लिए शाम (सीरिया) चले गए। लड़ाई को अभी ज़्यादा मुद्दत नहीं गुज़री थी कि ढाई साल की ख़िलाफ़त के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) का इंतिक़ाल हो गया। उन्हें रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क़ब्र के पास दफ़न किया गया।
हालाँकि हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों के सरदार और ख़लीफ़ा थे, लेकिन उनकी ज़िन्दगी बड़ी सादा थी। शुरू में वह अपना ख़र्च तिजारत करके पूरा करते थे, लेकिन बाद में मुसलमानों के मशविरे से सरकारी ख़ज़ाने से, जिसे 'बैतुलमाल' कहते थे, उनके लिए एक रक़म मुक़र्रर हो गई। वह ख़लीफ़ा होने के बावजूद मदीने की गलियों में चक्कर लगाकर लोगों के हालात मालूम करते थे और उनके निजी काम ख़ुद कर दिया करते थे।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो बाद में ख़लीफ़ा हुए, कहते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह एक बुढ़िया के घर जाकर उसके घर का काम कर दिया करता था, लेकिन एक रोज़ जब मैं गया तो बुढ़िया ने कहा कि आज कोई काम नहीं है। एक नेक आदमी तुमसे पहले आकर काम कर गया। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को बाद में मालूम हुआ कि यह हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे जो ख़लीफ़ा होने के बावजूद ग़रीब बुढ़िया के घर का काम कर आते थे।
हालाँकि हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सिर्फ़ ढाई साल हुकूमत की लेकिन उनका यह ज़माना इस्लामी इतिहास में बड़ी अहमियत रखता है। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) का यह बड़ा कारनामा है कि उन्होंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंतिक़ाल के बाद—
1. मुसलमानों में एकता क़ायम की,
2. अरब में होनेवाली बग़ावतों को कुचल दिया और,
3. हुकूमत को जल्दी ही इतना मज़बूत कर दिया कि मुसलमानों ने ईरान व रूम की हुकूमतों के ख़िलाफ़, जो उस ज़माने की सबसे बड़ी हुकूमतें थीं, एक साथ जिहाद शुरू करके उनके बहुत-से इलाक़े फ़तह कर लिए।
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) का एक और कारनामा क़ुरआन को संकलित करना है। क़ुरआन मजीद अब तक पूरा का पूरा एक जगह किताबी शक्ल में लिखा हुआ नहीं था। हाँ, हाफ़िज़ हज़ारों थे जिनको पूरा क़ुरआन याद था। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के प्रारम्भिक दौर में जब अरब में बग़ावतें हुईं तो कई सौ हाफ़िज़ लड़ाइयों में शहीद हो गए। सिर्फ़ एक जंग में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई थी सात सौ क़ुरआन के हाफ़िज़ शहीद हुए थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इसके बाद हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के मशविरे से पूरे क़ुरआन मजीद को एक जगह लिखवा लिया। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) चूँकि सिद्दीक़ के नाम से मशहूर थे, इसलिए क़ुरआन का यह नुस्ख़ा 'मुसहफ़े सिद्दीक़ी' कहलाता था। बाद में क़ुरआन के तमाम नुस्ख़े इसी मुसहफ़े सिद्दीक़ी से नक़ल किए गए।
हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनी ज़िंदगी ही में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपना जानशीन नामज़द कर दिया था। उन्होंने यह फ़ैसला मुसलमानों के मशविरे से किया था। मौत से पहले आपने हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हक़ में वसीयत लिखवाई और उसके बाद मसजिदे नबवी में जाकर, जहाँ तमाम मुसलमान जमा थे, लोगों से अपने इस फ़ैसले की एक बार फिर तसदीक़ (पुष्टि) कराई। आपने अवाम से पूछा—
"मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बल्कि उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर किया है तो क्या तुम लोग उनके चुनाव से राज़ी हो?"
और तमाम लोगों ने एक मत होकर हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के चयन को पसंद किया।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु)
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बड़े सहाबियों में से थे लेकिन वे इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के दुश्मन थे। एक दिन वे प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क़त्ल करने के इरादे से घर से निकले लेकिन ख़ुदा ने उन्हें ऐसी हिदायत दी कि वे क़त्ल करने के बजाय इस्लाम ले आए। वे बड़े बहादुर और निडर थे। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों की ताक़त बहुत बढ़ गई। मदीना पहुँचकर हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तरह हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने भी प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ तमाम बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़लीफ़ा मुक़र्रर हो जाने के बाद लड़ाई पूरे ज़ोर से शुरू हो गई। 'क़ादिसिया' के मैदान में एक सहाबी हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सिपहसालारी में तीस हज़ार मुसलमानों ने साठ हज़ार ईरानियों को पराजित किया और शाम (सीरिया) में 'यरमूक' के मैदान में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सिपहसालारी में चालीस हज़ार मुसलमानों ने एक लाख से ज़्यादा ईसाइयों को पराजित किया। मुसलमानों के जोश व ख़रोश का आतिशपरस्त (अग्निपूजक) ईरानी और ईसाई रूमी मुक़ाबला न कर सके, और कर भी कैसे सकते थे! मुसलमान समझते थे कि वे अपने लिए नहीं ख़ुदा के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया से बुराई को ख़त्म करने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। इसलिए उन्हें मौत का डर नहीं था। वे जानते थे कि ख़ुदा उन्हें इसका बदला देगा। यह भावना आतिशपरस्तों और ईसाइयों में नहीं थी। इसलिए वे हर जगह हारने लगे और मुसलमान हर जगह कामयाब होते गए। दस साल की मुद्दत में मुसलमानों ने ईरानी सल्तनत को ख़त्म कर दिया और रूमियों से शाम (सीरिया), फ़िलस्तीन और मिस्र (Egypt) के मुल्क छीन लिए।
इराक़ और ईरान की फ़तह
क़ादिसिया की जंग इस्लामी इतिहास में निर्णायक जंगों में गिनी जाती है। इस जंग में ईरानियों को ऐसी शिकस्त हुई कि वे अपनी राजधानी 'मदाइन' को भी नहीं बचा सके जो दजला नदी के पूर्वी तट पर उस जगह आबाद थी, जहाँ अब बग़दाद आबाद है। मुसलमान जब दजला के तट पर पहुँचे तो हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास ने अल्लाह का नाम लेकर अपना घोड़ा नदी में उतार दिया। अपने सरदार को आगे बढ़ते देख बाक़ी मुसलमानों ने भी अपने घोड़े नदी में डाल दिए और इस प्रकार पूरी फ़ौज बिना पुल के ही नदी पार कर गई। ईरानी यह समझते थे कि मुसलमान नदी को पार नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब मुसलमानों ने नदी को पार कर लिया तो उनके हाथ-पाँव फूल गए और ऐसे डरे कि 'देव आ गए, देव आ गए' कहते हुए भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने उनकी राजधानी मदाइन पर आसानी से क़बज़ा कर लिया। मुसलमानों ने अपनी इस शानदार कामयाबी पर सबसे पहले शुक्राना नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जुमा की नमाज़ 'किसरा' के शाही महल में अदा की।
हज़रत सअद ने जब शाही ख़ज़ाना और माल व असबाब मदीना रवाना किया तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) उसे देखकर रो पड़े। लोगों ने पूछा, "यह तो ख़ुशी की बात है, आप रोते क्यों हैं?" हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जवाब दिया, "मैं इसलिए रोता हूँ कि माल व दौलत की इस बहुतायत में मुझे मुसलमानों के ज़वाल (अवनति) के आसार नज़र आ रहे हैं।" मदाइन की फ़तह के बाद मुसलमान जल्द ही पूरे इराक़ और ख़ूज़िस्तान को इस्लामी हुकूमत के दायरे में ले आए।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) चाहते थे कि मुसलमान और आगे न बढ़ें। वह कहा करते थे कि काश, हमारे और ईरान के बीच आग का पहाड़ खड़ा हो जाता कि न हम ईरान पर हमला कर सकते और न ईरानी हमारे ऊपर! लेकिन ईरानी आतिशपरस्त बराबर हमले करते रहते थे जिसके कारण हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को मजबूर होकर चढ़ाई का हुक्म देना पड़ा। इराक़ और ईरान की सरहद के क़रीब नहावन्द के स्थान पर ईरानियों से फिर एक बड़ी जंग हुई। इस बार ईरानियों ने क़ादिसिया से भी ज़्यादा फ़ौज जमा कर ली थी। लेकिन मुसलमानों के मुक़ाबले में उनकी यह तादाद भी काम न आई। जंग में तीस हज़ार ईरानी काम आए और उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा। इस जंग में इस्लामी फ़ौज के सिपहसालार नोमान बिन मक़रन (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी शहीद हो गए। नहावन्द की इस जीत को 'फ़तहुल-फ़ुतूह' कहा जाता है, यानी ऐसी फ़तह जो कई फ़तहों (जीतों) के बराबर हो। नहावंद की हार ने ईरानियों की कमर तोड़ दी और वे इसके बाद कहीं भी जमकर मुक़ाबला नहीं कर सके। इस्लामी फ़ौज के विभिन्न दस्ते ईरान के विभिन्न हिस्सों की ओर रवाना कर दिए जो चार-पाँच साल के अन्दर-अन्दर पूरे ईरान को इस्लाम के राजनीतिक आधिपत्य में ले आए।
ईरान की फ़तह में जिन मुसलमान सिपहसालारों ने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए उनमें अहनफ़ बिन क़ैस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का नाम सबसे ऊपर है। जिस प्रकार हज़रत सअ्द (रज़ियल्लाहु अन्हु) फ़ातेहे-इराक़ कहलाते हैं उसी प्रकार अहनफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) फ़ातेहे ख़ुरासान कहलाते हैं। उन्होंने न केवल ख़ुरासान फ़तह किया, बल्कि सासानी हुक्मराँ 'यज़्दगर्द' को ईरान की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया और उस काम को पूरा कर दिया जो हज़रत ख़ालिद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने शुरू किया था। इस प्रकार प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की वह पेशनगोई (भविष्यवाणी) पूरी हो गई कि ईरान की सासानी सल्तनत टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। यज़्दगर्द के देश-निकाले के बाद ईरान के आतिशपरस्तों ने मुसलमानों से सुलह कर ली। हज़रत अहनफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इन कामयाबियों की ख़बर दी तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मुसलमानों को मसजिदे नबवी में जमा करके ख़ुशख़बरी सुनाई और कहा—
“आज आतिशपरस्तों की सल्तनत बरबाद हो गई। अब उनके मुल्क की एक चप्पा ज़मीन भी उनके क़बज़े में नहीं कि वे मुसलमानों को किसी प्रकार का नुक़्सान पहुँचा सकें। अल्लाह ने उनकी ज़मीन, उनका मुल्क और उनकी दौलत का तुम्हें वारिस (उत्तराधिकारी) बनाया है कि वह तुम्हें आज़माए। इसलिए तुम अपनी हालत न बदलो वरना ख़ुदा भी तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम को ले आएगा, मुझे उम्मत (यानी मुसलमानों) के लिए ख़ुद उसके अफ़राद (व्यक्तियों) से ख़ौफ़ है।"
शाम (Syria) व मिस्र (Egypt) की फ़तह
शाम व मिस्र की फ़तह के लिए मुसलमानों ने जो कारनामे अंजाम दिए वे ईरान की फ़तह से कम नहीं थे। रूम की सल्तनत दुनिया की शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी जाती थी और रूम का हुक्मराँ हिरक़्ल (Heraclius) शायद अपने दौर का सबसे बड़ा सिपहसालार था। उसने कुछ साल पहले ईरान के शहंशाह ख़ुसरो परवेज़ को लगातार पराजित किया था। लेकिन मुसलमानों के मुक़ाबले में हिरक़्ल भी बेबस हो गया। मुसलमानों की लगातार कामयाबियों को देखकर एक बार उसने अपने साथियों से पूछा—
"जब अरब तुमसे तादाद, असलहा (अस्त्र-शस्त्र) और साज़ो-सामान हर चीज़ में कम हैं तो फिर तुम उनके मुक़ाबले में कामयाब क्यों नहीं होते?"
एक व्यक्ति ने जवाब दिया—
“अरबों के अख़लाक़ हमारे अख़लाक़ से अच्छे हैं। वे रात को इबादत करते हैं और दिन में रोज़े रखते हैं, वे किसी पर ज़ुल्म नहीं करते, एक-दूसरे से बराबरी का सुलूक करते हैं। इसके विपरीत हमारा यह हाल है कि हम शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, वादे की पाबंदी नहीं करते, दूसरों पर ज़ुल्म करते हैं। इसका नतीजा यह है कि उनके हर काम में उत्साह और दृढ़ता होती है और हमारे काम इन गुणों से ख़ाली होते हैं।"
यरमूक की जंग क़ादिसिया की तरह निर्णायक साबित हुई। इसमें सत्तर हज़ार से लेकर एक लाख तक रूमी काम आए जबकि इसके मुक़ाबले में सिर्फ़ तीन हज़ार मुसलमान शहीद हुए। यह जंग हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हैरतअंगेज़ फ़ौजी सलाहियत का सबूत है जो इराक़ की शुरूआती जीतों के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हुक्म से शाम (सीरिया) आ गए थे और यहाँ इस्लामी फ़ौज की कमान संभाल ली थी। जब क़ैसरे-रूम हिरक़्ल को यरमूक के मैदान में रूमियों के पराजय की ख़बर मिली तो वह बड़ी हसरत और अफ़सोस के साथ शाम (सीरिया) को अलविदा कहकर क़ुस्तनतीनिया (Istambul) चला गया।
यरमूक की जंग के बाद हज़रत अबू उबैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस्लामी फ़ौज के सिपहसालार बना दिए गए और ख़ालिद बिन वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) उनके सहायक हो गए, लेकिन इसके बावजूद हज़रत ख़ालिद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने शाम (सीरिया) की लड़ाइयों में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया और थोड़े वक़्त में रूमियों को पूरे शाम (सीरिया) से निकाल दिया।
शाम (सीरिया) की फ़तह में एक अहम घटना “बैतुल-मक़्दिस" पर मुसलमानों का कब्ज़ा है। बैतुल-मक़्दिस जिसे यरूशलम भी कहा जाता है, शाम (सीरिया) के इलाक़े में फ़िलस्तीन में स्थित है। मुसलमानों का क़िब्ल-ए-अव्वल इसी शहर में था और यहीं वह स्थान है जहाँ से प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेराज के मौक़े पर आसमान की ओर रवाना हुए थे। जब मुसलमानों ने इस पवित्र शहर पर घेरा डाल दिया तो ईसाई इस शर्त पर शहर को हवाले करने और सुलह करने पर तैयार हो गए कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ख़ुद आकर सुलहनामा लिखें। जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इसकी सूचना दी गई तो वे तैयार हो गए और मदीना में हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपना जानशीन मुक़र्रर करके 'बैतुल मक़्दिस' की ओर रवाना हो गए। यह सफ़र उन्होंने इस सादगी से तय किया कि सिर्फ़ एक ग़ुलाम उनके साथ था और ऊँट पर वे दोनों बारी-बारी से बैठकर सफ़र करते थे। यानी एक बार हज़रत उमर बैठते और उनका ग़ुलाम पैदल चलता और दूसरी बार उनका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होता और हज़रत उमर ऊँट की नकेल पकड़कर पैदल चलते। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के कपड़े भी इतने सादा थे कि मुसलमान आपको उन कपड़ों के साथ शहर के वासियों के सामने पेश करते हुए झिझक रहे थे। लेकिन हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि हमारी इज़्ज़त इस्लाम की वजह से है, कपड़ों की वजह से नहीं। अतः आप उन्हीं कपड़ों में बैतुल मक़्दिस में दाख़िल हुए और ईसाइयों को एक सुलहनामा लिखकर दिया जिसमें उनके जान व माल और मज़हब की ज़मानत दी। उसी सुलहनामा की रू से हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने स्थानीय ईसाइयों के कहने पर यहूदियों को बैतुल मक़्दिस से निकाल दिया। अब मुसलमानों का क़िब्ल-ए-अव्वल भी उनके अपने क़ब्ज़े में आ गया। मुसलमानों ने हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की बनाई हुई मसजिद, जो 'हैकल सुलैमानी' कहलाती थी, का नवीनीकरण किया। यही मसजिद, 'मसजिदे अक़सा' कहलाती है।
हालाँकि शाम (सीरिया) और फ़िलस्तीन से रूमी निकाल दिए गए, लेकिन वे मिस्र की ओर से अब भी मुसलमानों के लिए ख़तरा हो सकते थे। एक मशहूर सहाबी हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, जो शाम (सीरिया) की लड़ाइयों में शरीक थे, हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से मिस्र पर हमला करने की इजाज़त माँगी इजाज़त मिलने पर उन्होंने दो-तीन साल के अन्दर पूरा मिस्र फ़तह कर लिया। रूमियों के ज़माने में बंदरगाह 'स्कंदरिया' मिम्र की राजधानी थी। अब मुसलमानों ने नील नदी के किनारे 'फ़िसतात' के नाम से एक नया शहर आबाद किया।
हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कुछ समय बाद पश्चिम में 'बरक़ा' (Cyrenaica) और 'तराबलस' (Tripolis) को भी इस्लामी ख़िलाफ़त की सीमा में शामिल कर लिया। यह वह इलाक़ा है जो आजकल 'लीबिया' कहलाता है।
सुधार
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कुल साढ़े दस साल ख़िलाफ़त की लेकिन इस अल्प अवधि में उन्होंने एक ऐसी विशाल हुकूमत क़ायम कर दी जो अपने क्षेत्रफल और शक्ति के लिहाज़ से अपने वक़्त की सबसे बड़ी हुकूमत थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का ज़माना सिर्फ़ जंग की कामयाबियों के कारण मशहूर नहीं है, बल्कि न्याय, इनसाफ़, प्रजा-पालन और शासन व्यवस्था की ख़ूबियों के कारण भी मशहूर है। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहद में पहली बार विभिन्न प्रशासन विभाग क़ायम किए गए और सरकारी आमदनी व ख़र्च का बाक़ायदा हिसाब तैयार किया गया। ये विभाग 'दीवान' कहलाते थे। प्रशासन व्यवस्था के सिलसिले में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जो क़दम उठाए और सुधार किए, उन्हें इस्लामी इतिहास में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की 'अव्वलियात' (प्राथमिकताएँ) कहा गया है, यानी वे काम जो सबसे पहले हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने किए। इन अव्वलियात की सूची बहुत लम्बी है। यहाँ संक्षिप्त सूची दी जा रही है, जिससे आपके द्वारा किए गए सुधार की अहमियत का अंदाज़ा होगा—
1. सल्तनत को सूबों (प्रांतों) में बाँटा।
2. फ़ौजी विभाग क़ायम किया।
3. वित्त विभाग क़ायम किया।
4. पुलिस विभाग क़ायम किया जिसे 'अहदास' कहा जाता था।
5. अदालतें क़ायम कीं।
6. बैतुलमाल क़ायम किया।
7. ज़मीन का माप करवाया।
8. जनगणना करवाई।
9. जेल क़ायम की।
10. ख़बरें हासिल करने के लिए पर्चानवीस मुक़र्रर किए।
11. फ़ौजी छावनियाँ क़ायम कीं।
12. इमामों और मुअज़्ज़िनों की तनख़्वाहें मुक़र्रर कीं।
13. मकतब और मदरसे क़ायम किए और उस्तादों की तनख़्वाहें मुक़र्रर कीं।
14. मक्का और मदीना के बीच चौकियाँ क़ायम कीं और सराएँ बनवाईं।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इन सुधारों के बाद इस्लामी ख़िलाफ़त जो पहले ही क्षेत्रफल के एतबार से दुनिया की एक बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, व्यवस्था और प्रशासनिक ढाँचे के लिहाज़ से भी अपने दौर की एक निहायत संगठित और व्यवस्थित हुकूमत में बदल गई।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का एक और बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने अपने शासनकाल में तमाम मुसलमानों के वज़ीफ़े मुक़र्रर कर दिए थे और वे इसे अपनी पूरी सल्तनत में फैला देना चाहते थे। इस बात को आप इतना महत्त्व देते थे कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर देते थे। पहले उन्होंने यह नियम बनाया था कि जब बच्चा दो साल का हो जाता था और माँ का दूध पीना छोड़ देता था तब वज़ीफ़ा मुक़र्रर किया जाता था, परन्तु एक रात जब वह मदीना में गश्त लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती। यह देखकर हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने औरत से पूछा, "तुम इस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती?"
औरत हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को नहीं पहचानती थी। उसने जवाब दिया—
"मैं इसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ क्योंकि उमर उस वक़्त तक वज़ीफ़ा मुक़र्रर नहीं करता जब तक बच्चा दूध न छोड़ दे।"
जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफ़सोस हुआ कि मेरे इस हुक्म के कारण न जाने कितने बच्चे माँ के दूध से महरूम (वंचित) रह जाते होंगे। इसके बाद उन्होंने हुक्म जारी किया कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया जाए।
वज़ीफ़ों का यह प्रबन्ध दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वुजूद में आया जो 'रफ़ाही मम्लकत' कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की ज़िम्मेदार होती है।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तरह 'बैतुल माल' का रुपया अपने ऊपर ख़र्च नहीं करते थे। वह 'बैतुल माल' को जनता की अमानत समझते थे। इसलिए उन्होंने अपनी तनख़्वाह मुक़र्रर कर ली थी और यह तनख़्वाह उतनी ही थी जो आम मुसलमानों की थी।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने लिए 'अमीरुल-मोमिनीन' का लक़ब इख़तियार किया। आपके बाद जितने ख़लीफ़ा हुए वे भी 'अमीरुल-मोमिनीन' कहलाए।
हालाँकि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनाया और न माल व दौलत जमा की। उनपर कोई भी शख़्स आरोप लगा सकता था और मुक़द्दमा चला सकता था। एक बार माले ग़नीमत [वह वस्तुएँ जो जंगों में जीतने के बाद प्राप्त होती थीं।] में चादरें भी आईं। ये चादरें मुसलमानों में बाँट दी गईं। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हिस्से में भी एक चादर आई। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) यह चादर ओढ़े मसजिद में तक़रीर दे रहे थे कि एक बद्दू (यानी देहाती अरब) उठा और उसने कहा, "उमर हम तुम्हारी बात उस वक़्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है?"
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसे बताया कि मेरे हिस्से की चादर चूँकि छोटी थी इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से की चादर लेकर जोड़ लिया है।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) इसका बहुत ख़याल रखते थे कि प्रजा पर ज़ुल्म न हो। मदीना में वे ख़ुद रातों को गश्त करते थे। हज के मौक़े पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुँचते थे तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) उनसे पूछा करते थे कि उनका हाकिम या शासक कैसे राज चलाता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौक़े पर हाज़िर होने का हुक्म था। जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) उससे जवाब तलब करते थे और शिकायत करनेवालों की शिकायत दूर करते थे।
हिजरी सन् जो इस्लामी दुनिया में राइज है हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का क़ायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्का से मदीना हिजरत की थी।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने शासनकाल में तीन शहर बसाए। उनके नाम कूफ़ा, बसरा और फ़िसतात हैं। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कृषि के विकास के लिए नहरें ख़ुदवाईं और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, प्रजा की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी (उत्तरदायित्व) के अहसास हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के वे कारनामे और ख़ूबियाँ हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश नहीं कर सकता।
यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको 'फ़ारूक़े आज़म' कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसा मिसाली नमूना बन गए जिसकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की—
यह मिसाली हुक्मरान साढ़े दस साल की ख़िलाफ़त के बाद एक ईरानी आतिशपरस्त अबू लूलू के ख़ंजर का शिकार हो गया। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि उस आतिशपरस्त ने उनपर हमला कर दिया और आप अत्यधिक ज़ख़्मों के कारण दूसरे दिन इन्तिक़ाल कर गए।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क़ब्र के पहलू में हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बराबर दफ़न किया गया।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु)
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने भी हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तरह अपने बाद अपनी औलाद या रिश्तेदारों में से किसी को अपना जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर नहीं किया। उन्होंने अपने इन्तिक़ाल से पहले छः आदमियों की एक समिति बना दी थी और कहा था कि ये लोग ख़ुद अपने में से एक ख़लीफ़ा चुन लें। उन्होंने यह हिदायत भी दी कि जो शख़्स मुसलमानों के मशविरे के बग़ैर ज़बरदस्ती अमीर (ख़लीफ़ा) बनने की कोशिश करे, उसे मौत की सज़ा दी जाए। उन बुज़ुर्गों के नाम, जो चुनाव समिति के सदस्य थे, ये हैं:-
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत सअ्द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु), और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु)।
ये तमाम बुज़ुर्ग अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथी थे। इस्लाम की इन्होंने बड़ी ख़िदमत की थी और ये उन दस लोगों में से थे जिन्हें प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जन्नत में जाने की ख़ुशख़बरी दी थी।
इस समिति ने आख़िरकार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लीफ़ा चुनने का अधिकार दे दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने आम लोगों से मिल-जुल कर उनका रुझान मालूम किया। उन्होंने हज से वापस होनेवाले क़ाफ़िलों से भी पूछा और आम जनता के विचार जानकर वह इस नतीजे पर पहुँचे कि लोग हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हक़ में हैं। अतः उन्होंने हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लीफ़ा बना दिया। चुनाव के बाद एक आम सभा में हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त की बैअत हुई।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी उन सहाबियों में हैं जो शुरू में इस्लाम ले आए थे। इन्होंने प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हर मौक़े पर साथ दिया। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) तिजारत करते थे और उनकी गिनती देश के धनवान लोगों में होती थी। उनकी दौलत से प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में एक बार आपने एक हज़ार ऊँट, पचास घोड़े और पूरी फ़ौज के लिए अनाज दिया।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दामाद भी थे। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी दो बेटियों हज़रत रुक़ैया (रज़ियल्लाहु अन्हा) और हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ियल्लाहु अन्हा) की शादी (एक के बाद दूसरी की) उनसे की थी। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जिस वक़्त ख़िलाफ़त मिली उस वक़्त उनकी उम्र सत्तर साल से ज़्यादा हो चुकी थी।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने (24 हि०/644 ई०-35हि०/655 ई०) तक़रीबन बारह साल ख़िलाफ़त की। उनके ज़माने में भी कई जंगों में विजय हासिल हुई और इस्लामी हुकूमत पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। पूरब में ग़ज़नी और काबुल तक का इलाक़ा मुसलमानों के क़बज़े में आ गया और पश्चिम में तूनिस (Tunish) पर, जो उस ज़माने में अफ़्रीक़ा कहलाता था, मुसलमानों का क़बज़ा हो गया। ईरान का आख़िरी बादशाह यज़्दगर्द हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ही के ज़माने में मारा गया और इस प्रकार उसकी ओर से मुसलमानों को इतमीनान हुआ। एशिया-ए-कोचक में भी फ़तह हासिल हुई।

चित्र 1 :- मशहूर सहाबी और इराक़ के फ़ातेह हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास के दारुल अमारा के खंडर जो हाल ही में कूफ़ा में खुदाई में मिले।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के काल का एक बड़ा कारनामा जलसेना की स्थापना है। अब तक मुसलमानों ने तमाम लड़ाइयाँ ज़मीन पर लड़ी थीं और वे समुद्री युद्ध से बिलकुल नावाक़िफ़ थे। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में मुसलमानों ने पहली बार समुद्री बेड़ा तैयार किया।
समुद्री बेड़ा तैयार करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि रूमी अगरचे शाम (सीरिया) और मिस्र से निकाल दिए गए थे, लेकिन उनके पास एक ताक़तवर समुद्री बेड़ा था जिसकी मदद से वे शाम और मिस्र के समुद्री तटों पर हमला करते रहते थे। इन हमलों की रोक-थाम के लिए शाम के गवर्नर अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से समुद्री बेड़ा बनाने की इजाज़त माँगी थी। परन्तु हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों को समुद्र के ख़तरों में डालना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी। बाद में हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इजाज़त दे दी। अतः अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने न केवल शाम के समुद्री तटों की कामयाब हिफ़ाज़त की बल्कि क़बरस (Cyprus) का टापू भी रूमियों से छीन लिया। इन समुद्री जंगों में अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अलावा मिस्र के गवर्नर अब्दुलाह बिन अबी सरह ने भी बड़ा नाम पैदा किया। उन्होंने दो सौ जंगी जहाज़ों से छः सौ जंगी जहाज़ों के रूमी बेड़े को पराजित किया। इस कामयाब समुद्री जंग के बाद इस्लामी ख़िलाफ़त रूम सागर की एक बड़ी समुद्री शक्ति बन गई।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जनता की सुविधा के लिए सड़कें, पुल और मुसाफ़िरख़ाने बनाए गए। उन्होंने मसजिदों में तनख़्वाहदार मुअज़्ज़िन (अज़ान पुकारनेवाला) रखे। मसजिदे नबवी को पुनः बनवाया और उसे ज़्यादा बड़ा और शानदार बनाया। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने लोगों के जो वज़ीफ़े मुक़र्रर किए थे, उन्हें जारी रखा। उनके ज़माने में भी हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने जैसी ख़ुशहाली रही।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) का एक और अहम कारनामा मुसलमानों को क़ुरआन को एक तरीक़े से पढ़ने पर सहमत करना है। क़ुरआन, हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने ही में पुस्तक रूप में संकलित हो गया था, परन्तु उसका प्रकाशन नहीं हुआ था। क़ुरआन के कुछ शब्दों की हिज्जे और उच्चारण भिन्न-भिन्न तरीक़ों से हो सकता है। अत: इन शब्दों को लोग अलग-अलग तरीक़े से लिखते और पढ़ते थे परन्तु इससे अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उस ज़माने में ग़ैर अरब लोगों ने बहुतायत से इस्लाम क़बूल किया। उनकी ज़बान चूँकि अरबी न थी, इसलिए उनमें क़ुरआन पढ़ने के तरीक़े पर मतभेद पैदा होने लगा। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह देखा तो हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जमा किया हुआ क़ुरआन का नुस्ख़ा जो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के पास सुरक्षित था, मंगाया और उसकी नक़लें करकर तमाम इस्लामी मुल्कों में भिजवा दीं, और उसके अलावा क़ुरआन के जो अन्य नुस्ख़े (प्रति) थे उन्हें नष्ट करा दिया। इस प्रकार हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ुरआन पर मतभेद का रास्ता बन्द कर दिया। इस वजह से हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को 'जामेअ क़ुरआन' (क़ुरआन को जमा करनेवाला) भी कहते हैं।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) बड़े मालदार थे, इसलिए वे आराम की ज़िंदगी गुज़ारते थे। सारा ख़र्च निजी आमदनी से पूरा करते थे, बैतुलमाल से कुछ नहीं लेते थे।
अपने निजी धन से सैकड़ों विधवाओं, अनाथों और सगे-सम्बन्धियों का पालन-पोषण करते थे और हर जुमा को एक ग़ुलाम ख़रीदकर आज़ाद करते थे। हया और शर्म एक मुसलमान के दीन का हिस्सा है और इस मामले में तमाम सहाबी मुसलमानों के लिए नमूना हैं, लेकिन हया और शर्म के मामले में हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) तमाम सहाबियों में सबसे आगे हैं। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमाया करते थे कि उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हया से तो फ़रिश्ते भी शरमाते हैं।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) बड़े नर्मदिल और दयालु इनसान थे। एक बार आपने किसी बात पर एक ग़ुलाम के कान ऐंठे, लेकिन बाद में इतना अफ़सोस हुआ कि अपने कान ग़ुलाम के सामने कर दिए और कहा, "लो तुम बदला ले लो।"
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने सगे-सम्बन्धियों का बहुत ख़याल रखते थे। वे कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ अच्छा व्यवहार करूँ। अतः हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) दूसरों के साथ अपने लोगों की भी मदद करते रहते थे और इस मक़सद के लिए निजी सम्पत्ति के अलावा बैतुलमाल से भी रक़म देते थे। उन्होंने हुकूमत में भी अपने लोगों को बड़े-बड़े ओहदे दिए। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस तरीक़े से कुछ लोगों में बेचैनी और शिकायत पैदा हुई। इस्लाम से पहले बनी हाशिम और बनी उमैय्या के क़बीलों में क़ुरैश की सरदारी के मसले पर दुश्मनी रहती थी। इस्लाम के बाद यह जज़्बा दब गया था। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का सम्बन्ध उनमें से किसी क़बीला से नहीं था और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी सरकारी ओहदे नहीं दिए थे। हज़रत उमर तो इस मामले में इतने सजग थे कि हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहा करते थे कि अगर आपमें से कोई ख़लीफ़ा हो जाए तो अपने क़बीलेवालों को मुसलमानों पर न थोपना। लेकिन हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ऐसा न कर सके। उनका सम्बन्ध बनी उमैय्या से था, इसलिए जब उन्होंने ख़ानदानवालों को बड़े-बड़े ओहदे दिए तो बनी हाशिम और बनी उमैय्या की सोई हुई दुश्मनी फिर जाग उठी। लोगों ने हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू किए। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) बादशाह या तानाशाह नहीं थे कि विरोध करनेवालों की ज़बान ज़बरदस्ती बन्द कर देते। उन्होंने आरोपों की तहक़ीक़ के लिए एक निष्पक्ष समिति बनाई जिसने इराक़, शाम और मिस्र जाकर मामलात की तहक़ीक़ात की और तमाम आरोपों को बेबुनियाद क़रार दिया। लेकिन हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की नर्मदिली, नेकी और बुढ़ापे से उनके कुछ रिश्तेदारों ने विशेषकर उनके कातिब मरवान बिन हकम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और फ़ितने की आग फिर भड़क उठी।
हंगामा पैदा करनेवाले लोग मदीना के नहीं थे। उनका सम्बन्ध बसरा, कूफ़ा और मिस्र के उन गिरोहों से था जिनकी सही इस्लामी तरबियत नहीं हुई थी। उनमें कोई बड़ा प्रतिष्ठित आदमी नहीं था और उनकी तादाद भी दो हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। ये लोग अचानक मदीना में घुस आए। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के मकान को घेर लिया और उनसे ख़िलाफ़त छोड़ देने की माँग की। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तलवार के ज़ोर से ख़लीफ़ा नहीं बना हूँ कि मुझे ज़बरदस्ती हटाया जाए। मैं मुसलमानों की मरज़ी से ख़लीफ़ा चुना गया हूँ। इस मौक़े पर कुछ सहाबियों ने हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को हंगामा करनेवालों के ख़िलाफ़ ताक़त इस्तेमाल करने का मशविरा भी दिया, लेकिन उन्होंने यह मशविरा क़बूल नहीं किया और कहा कि मैं अपनी वजह से मुसलमानों में ख़ून-ख़राबा की शुरूआत करना नहीं चाहता। वे इस फ़ैसले पर अन्तिम वक़्त तक जमे रहे यहाँ तक कि बलवाइयों ने घर में घुसकर आपको शहीद कर दिया।
"हक़ीक़त यह है कि इस अत्यन्त नाज़ुक मौक़े पर हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने वह नीति अपनाई जो एक ख़लीफ़ा और एक बादशाह के फ़र्क़ को नुमाया करती है। उनकी जगह कोई बादशाह होता तो अपने शासन को बचाने के लिए कोई बाज़ी खेल जाने में भी उसे संकोच न होता, चाहे कितनी ही तबाही और बरबादी होती। मगर वे तो सच्चे ख़लीफ़ा थे। अपनी जान देने को इससे हल्की चीज़ समझते थे कि उनके कारण उन प्रतिष्ठाओं का अनादर हो जो एक मुसलमान को हर चीज़ से बढ़कर प्रिय होनी चाहिए।"
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु)
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की शहादत के बाद बलवाइयों ने हज़रत तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से ख़िलाफ़त क़बूल करने को कहा, लेकिन हर एक ने इनकार कर दिया। आख़िरकार मदीनावासी हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास गए और कहा कि ख़िलाफ़त का निज़ाम किसी अमीर के बग़ैर क़ायम नहीं रह सकता और आज आपके सिवा कोई और शख़्स इस ओहदे के योग्य नहीं है। आख़िरकार हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़िलाफ़त क़बूल कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बैअत गुप्त रूप से नहीं हो सकती। इसलिए आम मुसलमानों की सहमति ज़रूरी है। अतः मसजिदे नबवी में एक आम सभा हुई और सतरह या बाईस सहाबा के अलावा तमाम मदीनावासियों ने उनके हाथ पर बैअत कर ली।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। वे दस वर्ष की उम्र में ही इस्लाम ले आए थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने की जंगों में सबसे ज़्यादा बहादुरी का प्रदर्शन उन्होंने ही किया था। इसी लिए मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें हैदर (शेर) का ख़िताब दिया था और एक तलवार दी जिसे ज़ुल्फ़िक़ार कहते हैं। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में वे तमाम अहम फ़ैसलों में सम्मिलित रहे। वे हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को भी अहम मौक़ों पर मशविरा देते थे।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त बड़ी मुश्किल और पेचीदा परिस्थितियों में शुरू हुई। ख़लीफ़ा बनने के बाद हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) का पहला काम हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के क़ातिलों को सज़ा देना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि किसी क़ातिल का नाम मालूम नहीं था और बलवाई, जो हज़ारों की तादाद में थे, मदीना पर छाए हुए थे और बहुत-से ऐसे थे जो फ़ौज में शामिल हो गए थे। इस मुश्किल के कारण हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपराधियों को तुरन्त सज़ा नहीं दे सकते थे। परन्तु उनकी इस मजबूरी को बहुत-से मुसलमानों ने नहीं समझा और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से जल्द से जल्द अपराधियों को दण्डित करने की माँग करने लगे। सज़ा के लिए आग्रह करनेवालों में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की प्यारी बीवी हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) और हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) व हज़रत तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसे बुज़ुर्ग सहाबी भी थे।
ये लोग हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के नेतृत्व में फ़ौज लेकर बसरा की ओर रवाना हो गए जहाँ उनके हामियों (समर्थकों) की संख्या ज़्यादा थी। इसी दौरान हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी वहाँ पहुँच गए। बसरा के निकट जब दोनों फ़ौजें आमने-सामने हुईं तो हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की ओर से कुछ माँगें रखी गईं। दूसरी ओर हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनी मुश्किलें बताईं। चूँकि दोनों ओर से साफ़ दिल से कोशिश हो रही थी, इसलिए जल्दी ही सुलह हो गई। हज़रत तलहा (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) वापस हो गए और हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने भी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। परन्तु बलवाई जो दोनों फ़ौजों में मौजूद थे इस सुलह से घबरा गए और उन्होंने एक रात दोनों ओर की फ़ौजों पर हमला कर दिया। अब दोनों फ़ौजों को एक-दूसरे पर संदेह हुआ कि उनपर धोखे से हमला किया गया है। इस प्रकार जंग हुई और इस जंग में हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को फ़तह हुई। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को तमाम हालात से बाख़बर कर दिया और वह संतुष्ट होकर वापस चली गईं।
यह लड़ाई 'जंगे जमल' के नाम से मशहूर है क्योंकि हज़रत आइशा ऊँट पर सवार थीं और ऊँट को अरबी में 'जमल' कहते हैं। जंगे जमल के बाद हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) मदीना वापस नहीं आए और कूफ़ा को ही अपनी राजधानी बना लिया।
जंगे जमल पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने आपस में एक-दूसरे का ख़ून बहाया। मुसलमान आपस के इस टकराव से बड़े दुखी थे। उन्हें इतना अफ़सोस था कि कुछ सहाबा ने लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था और जब हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की फ़ौजें मदीना से रवाना हुईं तो मदीना के लोग फूट-फूटकर रो रहे थे।
हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सुलह हो गई, लेकिन शाम (सीरिया) के गवर्नर अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) से सुलह नहीं हो सकी। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उन्हें शाम से अपदस्थ कर दिया था, लेकिन उन्होंने हुक्म नहीं माना और कहा कि जब तक हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) का क़सास (हत्या का बदला) नहीं लिया जाएगा मैं ख़िलाफ़त तसलीम नहीं करूँगा।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अमीर मुआविआ के दरमियान सिफ़्फ़ीन के मुक़ाम पर जंगे जमल से भी बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें दोनों ओर से नब्बे हज़ार मुसलमान शहीद हुए, लेकिन इसके बाद भी कोई फ़ैसला न हो सका।
सिफ़्फ़ीन के आख़िरी मारके (लड़ाई) में जो लैलतुल-लहर कहलाता है। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) तक़रीबन कामयाबी हासिल कर चुके थे, लेकिन अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जब देखा कि उनकी फ़ौज हार जाएगी तो क़ुरआन को बीच में वास्ता बनाया। उनकी फ़ौजों ने अपने भालों से क़ुरआन बांधकर बुलंद किए और कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इसके (क़ुरआन के) मुताबिक़ फ़ैसला होना चाहिए। अतः लड़ाई बंद कर दी गई और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ओर से अबू मूसा अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ओर से अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) मध्यस्थ बनाए गए और तय पाया कि ये दोनों जो फ़ैसला करेंगे, हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को मंज़ूर होगा। 'दूमतुल-जन्दल' नामक स्थान पर मुसलमानों की बहुत बड़ी सभा हुई, लेकिन अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) की वादाख़िलाफ़ी के कारण जो उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के साथ की, यह सभा किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी और मुसलमान वहाँ से मायूस लौटे। बहरहाल इसके बाद हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने आपस के ख़ून-ख़राबे बंद करने की सुलह कर ली।
उस ज़माने में मुसलमानों में एक नया फ़िरक़ा (सम्प्रदाय) पैदा हुआ जो 'ख़ारजी' कहलाता है। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के समर्थकों में कुछ लोगों का कहना था कि दीनी मामलात में इनसान को मध्यस्थ बनाना कुफ़्र है और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अबू मूसा अशअरी को मध्यस्थ बनाने का जो फ़ैसला किया है वह क़ुरआन के विपरीत है। अतः ये लोग हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से अलग हो गए। ये ख़ारजी अतिवादी थे और आतंक एवं हिंसा पर इनका यक़ीन था। अतः उनहोंने एक भयंकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु), अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों में ख़ानाजंगी के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए इन्हें क़त्ल कर देना चाहिए। अतः कुछ दिनों के बाद एक निश्चित दिन तीन ख़ारजी इस मक़सद से अपने-अपने घरों से निकले। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) तो किसी तरह बच गए लेकिन तीसरे ख़ारजी ने जिसका नाम इब्ने मलजम था, हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जबकि वह फ़ज्र की नामज़ पढ़ने मस्जिद जा रहे थे, शहीद कर दिया।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने तक़रीबन साढ़े चार साल ख़िलाफ़त की। शाम और मिस्र के अलावा बाक़ी तमाम सलतनत उनके क़बज़े में थी। चूँकि उनका ज़माना ज़्यादातर ख़ानाजंगी में गुज़रा इसलिए कोई नया मुल्क फ़तह नहीं किया गया।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की शासन व्यवस्था बहुत हद तक हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसी थी। उनकी ज़िन्दगी भी उन्हीं की तरह सादा थी। फ़ैसला करते समय वे बड़े से बड़े आदमी की, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों की भी रियायत नहीं करते थे। वे ख़ुद को आम जनता के बराबर समझते थे और हमेशा जवाबदेही के लिए तैयार रहते थे। एक बार एक यहूदी ने उनकी ज़िरह चुरा ली। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसे देखकर पहचान लिया। यदि वे चाहते तो उस यहूदी से ज़िरह ज़बरदस्ती छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और क़ानून के मुताबिक़ यहूदी पर अदालत में दावा किया। क़ाज़ी भी इनसाफ़ के मामले में सख़्त थे। उन्होंने हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से सबूत माँगा। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) सबूत न दे सके। अतः क़ाज़ी ने यहूदी के पक्ष में फ़ैसला सुना दिया। इस फ़ैसले का यहूदी पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह मुसलमान हो गया और कहा, “यह तो नबियों जैसा इनसाफ़ है। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) अमीरूल मोमिनीन होकर मुझे अपनी अदालत के क़ाज़ी के सामने पेश करते हैं और क़ाज़ी अमीरूल मोमिनीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है।"
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने बाद किसी को जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर नहीं किया। लोगों ने जब आपके बड़े बेटे हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लीफ़ा बनाने के सम्बन्ध में पूछा तो आपने कहा, “न मैं तुम लोगों को इसका हुक्म देता हूँ और न इससे रोकता हूँ।" एक और शख़्स ने जब सवाल किया कि आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्यों नहीं कर देते तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं मुसलमानों को उसी हालत में छोड़ूँगा जिस हालत में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने छोड़ा था।"
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इन्तिक़ाल के बाद कूफ़ा के लोगों ने आपके बेटे हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लीफ़ा चुन लिया। हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों में ख़ून-ख़राबे को पसन्द नहीं करते थे, इसलिए जब अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इराक़ पर हमला किया तो उन्होंने जंग करने के बदले अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के लिए ख़िलाफ़त छोड़ दी। इस प्रकार हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बेमिसाल क़ुरबानी ने मुसलमानों को ख़ानाजंगी से निजात दिला दी। ख़िलाफ़त से हटने के बाद हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) कूफ़ा छोड़कर मदीना आ गए और वहीं नौ साल बाद 50 हिज०/670 ई० में इन्तिक़ाल किया। आपकी ख़िलाफ़त छः महीने रही।
ख़लीफ़ाओं का कार्यकाल
1. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) - 11 हि०/632 ई० से 13 हि०/634 ई०
2. हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) - 13 हि०/634 ई० से 24 हि०/645 ई०
3. हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) - 24 हि०/645 ई० से 35 हि०/655 ई०
4. हज़रत अली मुर्तज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) - 35 हि०/655 ई० से 40 हि०/660 ई०
जंगें
जंगे यरमूक - 13हि०/634 ई०
जंगे क़ादसिया - 15 हि०/636 ई०
फ़तह मिस्र - 21 हि०/641 ई०
जंगे नहावंद – 21 हि०/642 ई०
जंगे जमल - 36 हि०/656 ई०
जंगे सिफ़्फ़ीन - 36-37 हि०/657 ई०
अध्याय-7
ख़िलाफ़ते राशिदा
एक प्रजातांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी रियासत
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की शहादत और ज़्यादा सही यह है कि हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़िलाफ़त से हटने के साथ इस्लामी इतिहास का दूसरा अहम दौर ख़त्म हो गया। पहला दौर अहदे रिसालत का दौर (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दौर) था जिसमें सारे अरब में इस्लाम फैला, इस्लामी समाज वुजूद में आया और इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी। दूसरा दौर जो हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त से शुरू हुआ और हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़िलाफ़त से हटने तक चला। इसे बाद के इतिहासकारों ने ख़िलाफ़ते राशिदा का नाम दिया यानी सीधे रास्ते पर चलनेवाली ख़िलाफ़त। इस दौर में इस्लामी हुकूमत ने अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत प्राप्त कर ली और इस्लामी ख़िलाफ़त एक विश्व-व्यापी शक्ति बन गई।
ख़िलाफ़ते राशिदा का राजनीतिक ढाँचा बड़ी हद तक वही था जिसकी चर्चा हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हालात में हो चुकी है। यहाँ ख़िलाफ़ते राशिदा के सिर्फ़ उन्हीं पहलुओं की चर्चा की जा रही है, जिनके कारण विश्व इतिहास में ख़िलाफ़ते राशिदा की सबसे अलग पहचान बन सकी है और वह सबसे श्रेष्ठ नज़र आती है।
प्रशासन व्यवस्था, राजनीति और समाज सुधार के मैदान में इन तीस सालों में जो कारनामे अंजाम दिए गए वे न केवल इस्लामी इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में संगे मील (मील के पत्थर) की हैसियत रखते हैं। ख़िलाफ़ते राशिदा की राजनीतिक व्यवस्था और सामूहिक जीवन व्यवस्था की बुनियाद वही थी जो अहदे रिसालत में रखी गई थी, लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में इस बुनियाद पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी गई और दुनिया को यह बता दिया गया कि इस्लाम की राजनीतिक और सामूहिक जीवन व्यवस्था सिर्फ़ अरब प्रायद्वीप के ख़ानाबदोश लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद पर अपने वक़्त की आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की बुनियादें भी रखी जा सकती हैं। इतिहास का अध्ययन बताता है कि ख़ानाबदोश अरबों की तरह ईरान, ईराक़, शाम (सीरिया) और मिस्र के सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों के लिए भी इस्लाम रहमत और भलाई का पैग़ाम साबित हुआ।
बादशाहत नहीं ख़िलाफ़त
यूनान और रूम के इतिहास के एक अल्प काल को छोड़कर, प्राचीन काल से लेकर फ़्रांस की क्रांति (1789 ई०) तक दुनिया की एक मात्र शासन व्यवस्था बादशाहत रही है। ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में भी दुनिया के हर मुल्क में बादशाहत क़ायम थी, लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा की राजनीतिक व्यवस्था उन सबसे भिन्न थी और बादशाहत से उसका दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं था। इसमें शक नहीं कि :
“हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी जानशीनी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया था, लेकिन मुसलमानों ने यह जान लिया था कि इस्लाम एक शूराई ख़िलाफ़त का तक़ाज़ा करता है। इसलिए वहाँ न किसी ख़ानदानी बादशाहत की बुनियाद डाली गई और न कोई शख़्स ताक़त इस्तेमाल करके ख़लीफ़ा बना। न ही किसी ने ख़िलाफ़त हासिल करने के लिए कोई दौड़-धूप की, बल्कि एक के बाद दूसरे चार साहाबा को लोग अपनी आज़ाद मरज़ी से ख़लीफ़ा बनाते चले गए। इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात ज़ाहिर हो जाती है कि मुसलामनों की नज़र में ख़िलाफ़त का तरीक़ा यही है।"
एक प्रसिद्ध सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, जो ख़िलाफ़ते राशिदा में उच्च पदों पर रहे हैं, ख़िलाफ़त और बादशाहत के फ़र्क़ को इस तरह बयान किया है—
"ख़िलाफ़त वह है जिसे क़ायम करने में मशविरा किया गया हो और बादशाही वह है जिसपर तलवार के ज़ोर से क़बज़ा किया जाता है।"
खिलाफ़ते राशिदा का जो राजनीतिक ढाँचा था वह प्रजातंत्र की ठेट पश्चिमी परिभाषा के अनुसार प्रजातांत्रिक नहीं था, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता प्रजा को प्राप्त नहीं थी। फिर भी वह हर दौर की प्रजातंत्र के मुक़ाबले में ज़्यादा प्रजातांत्रिक था। यहाँ तक कि आधुनिक पश्चिमी एवं साम्यवादी सरकारों के मुक़ाबले में भी ज़्यादा प्रजातांत्रिक था। इसका कारण यह था कि इस राजनीतिक व्यवस्था में हाकमीयत (सम्पूर्ण प्रभुत्त्व) सिर्फ़ अल्लाह को प्राप्त था। अल्लाह और रसूल के बाद प्रजा को सारे अधिकार प्राप्त थे और वे क़ुरआन व सुन्नत के तय किए गए उसूलों के दायरे में पूर्णरूप से स्वतन्त्र थे। अल्लाह की हाकमीयत ने ख़िलाफ़ते राशिदा के इस्लामी समाज को न केवल उन ज़ुल्मों और नाइनसाफ़ियों से छुटकारा दिला दिया था जो बादशाही हुकूमतों का लाज़िमी नतीजा होते हैं, बल्कि उन ज़ुल्मों, बेइनसाफ़ियों और गुमराहियों से भी बचा लिया जो आधुनिक काल में प्रजा की हाकमीयत (यानी प्रजातन्त्र) के नाम पर आम हैं और जिनके कारण न केवल दूसरी क़ौमों को नुक़सान पहुँचता है, बल्कि ख़ुद अपनी क़ौम भी नुक़सान उठाती है। [अमेरिका में 1920 ई० में शराब पर पाबंदी लगाई गयी थी लेकिन आख़िरकार जनता की माँग पर 1933 ई० में यह क़ानून रद्द कर दिया गया। ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में या किसी इस्लामी रियासत में अवाम की माँग पर ऐसा करना मुमकिन नहीं। इसी प्रकार साम्यवादी देशों में अदालती कार्रवाई के बग़ैर लोगों की मिल्कियत को बिना मूल्य जिस प्रकार छीना जाता है और साम्यवाद से असहमति जतानेवालों की ज़बान बंद की जाती है तथा साम्यवाद ज़बर्दस्ती थोपे जाते हैं, ख़िलाफ़ते राशिदा में ऐसा करना मुमकिन नहीं था।]
सलाहकार कमेटी की प्रथा
प्रजातन्त्र की आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है और यह विशेषता ख़िलाफ़ते राशिदा में पूरी तरह मौजूद थी। ख़लीफ़ा को रियासत के प्रशासक की हैसियसत से पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। परन्तु वह दो बातों का पाबन्द था— एक इस्लामी क़ानून की पाबन्दी और दूसरी सलाह देने योग्य लोगों से मशविरा करना। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़लीफ़ा बनने के बाद पहले ख़ुतबे (अभिभाषण) ही में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि वह क़ुरआन व सुन्नत की पाबन्दी न करें तो लोगों के लिए उनका आज्ञापालन अनिवार्य नहीं। इसी प्रकार आपसी मशविरे के सम्बन्ध में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का मशहूर क़ौल (कथन) है कि ख़िलाफ़त के लिए मशविरा लाज़िम (अनिवार्य) है। अतः ख़िलाफ़ते राशिदा के पूरे दौर का इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई ख़लीफ़ा प्रशासन व्यवस्था और क़ानून बनाने के मामले में मुसलमानों में योग्य व्यक्तियों से मशविरा किए बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं करता था। लोगों को अपने विचार बताने की पूरी आज़ादी थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) तो लोगों का हौसला बढ़ाते थे कि वे आज़ादी के साथ अपने विचार रखें। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का यह नियम था कि जब कोई अहम मसला पेश आता था तो वह एलान करा देते थे कि लोग मस्जिदे नबवी में जमा हो जाएँ। जब लोग मस्जिद में जमा हो जाते तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) दो रकअत नमाज़ पढ़ते और फिर हाज़िर लोगों के सामने मसला पेश करके उनका मशविरा तलब करते। कभी-कभी बहस लम्बी छिड़ जाती और कई-कई दिन जारी रहती। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) पर तमाम ख़लीफ़ाओं में सबसे ज़्यादा आलोचना की गई और इल्ज़ाम लगाए गए, पर आपने कभी किसी का मुँह ज़बर्दस्ती बन्द करने की कोशिश नहीं की और अपने ऊपर लगाए जानेवाले इल्ज़ामों की सार्वजनिक रूप से सफ़ाई पेश की।
क़ानून की बालादस्ती
आपसी सलाह व मशविरा और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के बाद ख़िलाफ़ते राशिदा की एक और विशेषता, क़ानून की बालादस्ती थी। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा न्याय व इनसाफ़ तभी संभव है जब क़ानून लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करे। ख़िलाफ़ते राशिदा में इनसाफ़ के लिए हर जगह अदालतें क़ायम थीं जहाँ क़ाज़ियों (जजों) के सामने मुक़द्दमे पेश किए जाते थे। उस ज़माने में जज को 'क़ाज़ी' कहा जाता था। हालाँकि क़ाज़ियों की नियुक्ति ख़लीफ़ा करता था, परन्तु वे अपने फ़ैसलों में बिलकुल आज़ाद होते थे। यहाँ तक कि वे ख़ुद ख़लीफ़ा के ख़िलाफ़ मुक़द्दमे की सुनवाई कर सकते थे। पिछले अध्याय में इसकी मिसालें पेश की जा चुकी हैं कि ख़लीफ़ा तक को किस प्रकार अदालत में तलब कर लिया जाता था। हक़ीक़त यह है इस दौर में क़ाज़ियों को सख़्त हिदायत थी कि वे अपने फ़ैसलों में किसी के साथ रिआयत न करें, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ानून की बालादस्ती की एक मिसाल इस प्रकार क़ायम की कि जब उनके बेटे अबू शहमा शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए तो उन्हें क़ानून के मुताबिक़ कोड़े मारे गए और वह इस मार की चोट को बरदाश्त न कर सके और थोड़े दिन बाद इन्तिक़ाल कर गए।
हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में एक बार लोग एक ख़ारजी को पकड़ लाए जो खुले तौर पर कह रहा था कि मैं अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को क़त्ल कर दूँगा। परन्तु हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने यह कहकर उसे रिहा कर दिया कि जब तक वह कोई व्यावहारिक कार्रवाई नहीं करता, मात्र ज़बानी विरोध जताना कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसके कारण उसे सज़ा दी जाए।
दुनिया का इतिहास ऐसी मिसालों से ख़ाली है। ये मात्र चंद मिसालें नहीं हैं, बल्कि उस ज़माने की जीती-जागती तस्वीरें हैं और यह सब कुछ केवल उसी जीवन व्यवस्था में संभव है जिसमें क़ानून की बरतरी (सर्वोच्चता) हो और उसके साथ अल्लाह के यहाँ जवाबदेही की कल्पना हो।
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन न केवल निजी रूप से न्याय एवं इनसाफ़ को महत्त्व देते थे, बल्कि प्रांतों और ज़िलों के हाकिमों को भी इसके लिए निर्देश देते थे कि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं—
“मैंने अपने हाकिमों को इसलिए मुक़र्रर नहीं किया है कि वे लोगों को पीटें और उनका माल छीनें, बल्कि इसलिए मुक़र्रर किया है कि वे लोगों को दीन और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का तरीक़ा सिखाएँ। यदि किसी हाकिम ने इसके ख़िलाफ़ काम किया हो तो मेरे सामने शिकायत की जाए। ख़ुदा की क़सम मैं उसे सज़ा दूँगा।"
हाकिमों से जवाब तलबी का यह तरीक़ा आख़िर तक क़ायम रहा। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में वह सख़्ती तो नहीं रही जो हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में थी, लेकिन उस ज़माने में भी हाकिम जवाब तलबी से नहीं बच सकते थे। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में गवर्नरों को हिदायत थी कि वे हज के मौक़े पर मक्का में हाज़िर हुआ करें। इस मौक़े पर चूँकि रियासत के हर हिस्से से लोग मक्का पहुँचते थे, इसलिए लोगों की शिकायत सुनना और उनके हाकिमों से जवाब तलब करना आसान था।
आर्थिक न्याय
आर्थिक न्याय भी इनसानी समाज की बुनियादी ज़रूरत है और ख़िलाफ़ते राशिदा में इसपर पूरी तवज्जोह दी गई। उस ज़माने में सरकारी आमदनी के पाँच बड़े ज़रिये (स्रोत) थे। ज़मीनों का ख़िराज और जिज़्या— ये दोनों टेक्स ग़ैर मुस्लिमों से लिए जाते थे। उश्र, जो कृषि उत्पाद पर टैक्स था और ज़कात जो मुसलमानों से वसूल की जाती थी और माले ग़नीमत। चूँकि उस ज़माने में मुसलमानों ने कई जंगें जीतीं, इसलिए माले ग़नीमत भी आमदनी का बड़ा ज़रिया था। माले ग़नीमत के पाँच हिस्से कर दिए जाते थे। चार हिस्से फ़ौजियों में बाँट दिए जाते थे और पाँचवाँ हिस्सा केन्द्रिय ख़िलाफ़त को भेज दिया जाता था जो केन्द्रिय बैतुलमाल (ख़ज़ाना) में जमा हो जाता था। इस प्रकार हर मुल्क और सूबे की स्थानीय आमदनी पहले स्थानीय ज़रूरतों पर ख़र्च होती थी और जो अतिरिक्त बच जाता उसे केन्द्रिय बैतुलमाल के लिए भेज दिया जाता था। बैतुलमाल की रक़म क़ौम की अमानत समझी जाती थी। ख़लीफ़ा इस रक़म को न अपने आप पर ख़र्च करते थे और न अपने रिश्तेदारों पर। ख़लीफ़ा के अपने ख़र्चे के लिए उनकी तनख़्वाहें मुक़र्रर होती थीं और यदि उन्हें कभी तनख़्वाह के अलावा पैसे की ज़रूरत होती थी तो वह उसे लेने से पहले अवाम से इजाज़त लेते थे। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) चूँकि दौलतमंद थे, इसलिए वह बैतुलमाल से कोई तनख़्वाह नहीं लेते थे। बैतुलमाल को जिस प्रकार ख़लीफ़ा ने क़ौम की अमानत समझा और इस सम्बन्ध में जिस ज़िम्मेदारी के अहसास का सबूत दिया उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। इसी तरह ख़लीफ़ाओं के ज़माने में धन का वितरण जिस न्यायसंगत ढंग से करने की कोशिश की गई, वह भी अपनी मिसाल आप है। तिजारत और कारोबार में सूद नहीं लिया जाता था। जो लोग तिजारत करते थे वह इस बात का ख़याल रखते थे कि उनकी आमदनी में हराम माल शामिल न हो। हुकूमत दौलतमंद लोगों से ज़कात ख़ुद वुसूलती थी और उसकी रक़म ज़रूरतमंदों की मदद एवं दूसरे अच्छे कामों पर ख़र्च करती थी। जो शख़्स मुहताज हो जाता था उसका ख़र्च हुकूमत ख़ुद उठाती थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में अरब के मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों और ग़ुलामों के जिस प्रकार वज़ीफ़े मुक़र्रर किए गए वह अवाम की आर्थिक सहयोग की ऐसी पद्धति थी जिसकी मिसाल न तो इस्लाम से पहले के इतिहास में मिलती है और न बाद के इतिहास में। यह पद्धति हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने तक, बल्कि उसके बाद भी जारी रही।
ख़िलाफ़ते राशिदा की यही विशेषताएँ थीं जिनके कारण प्रसिद्ध अंग्रेज़ इतिहासकार एच० जी० वेल्ज़ ने लिखा है—
"इस्लाम को दूसरी क़ौमों पर ग़लबा (आधिपत्य) इसलिए हासिल हुआ कि वह अपने ज़माने में सबसे अच्छी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी।"
जंगों में जिहाद की रूह
जंग और साम्राज्य विस्तार से सम्बन्धित इस्लाम के नज़रिये को अहदे रिसालत वाले अध्याय में बयान किया जा चुका है। इस्लाम में जंग सिर्फ़ ख़ुदा की राह में जायज़ है और इसी लिए इस्लामी जंग को 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' कहा जाता है। ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में इस्लामी जंगी क़ानून पर पूरा-पूरा अमल किया गया और इस तरह जंग की तबाही को कम से कम करने की कोशिश की गई। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बाद जब ईरान और रूम से लड़ाई शुरू हो गई तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इन लड़ाइयों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की हर संभव कोशिश की। इराक़ की फ़तह के बाद वह नहीं चाहते थे कि जंग ईरान तक फैले। इसी प्रकार उन्होंने मिस्र पर चढ़ाई करने की इजाज़त मजबूर होकर दी। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में भी ज़्यादातर लड़ाइयाँ बग़ावतों को कुचलने के लिए हुईं या उन लड़ाइयों को एक निश्चित परिणाम तक पहुँचाने के लिए की गईं जो पहले से शुरू हो चुकी थीं।
मुसलमानों का तरीक़ा था कि लड़ाई शुरू करने से पहले दुश्मन को इस्लाम की दावत देते थे [जंग के शुरू में इस्लाम की इस दावत का कुछ ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने ग़लत मतलब निकाला है और यह इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। हालांकि इस्लाम की यह पेशकश जंग का एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश थी और तीन शर्तों में से एक शर्त थी। इसके जवाब में कभी किसी ने इस्लाम क़बूल नहीं किया और इतिहास बताता है कि मैदाने जंग में फ़तह हासिल करने के बाद दुश्मन के किसी क़ैदी या नागरिक को इस्लाम क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया गया। ईरान, इराक़, शाम और मिस्र के वासियों ने लगभग एक सौ साल की अवधि में बग़ैर किसी दबाव के इस्लाम क़बूल किया। इस्लाम की सीधी और सरल शिक्षाएँ, मुसलमानों का श्रेष्ठ आचरण और पूर्व प्रशासकों के मुक़ाबले में मुसलमानों का सद्व्यवहार इन क़ौमों में इस्लाम के प्रसार का कारण बना। दीन के मामले में इस्लाम की शिक्षा यह है कि शक्ति से किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता।] और जब वह इनकार कर देता तो इस्लामी रियासत का आज्ञापालक बनने को कहते थे और जंग तभी शुरू करते थे जब दुश्मन इन दो बातों को रद्द कर देता था। यह दुनिया की तारीख़ में बिलकुल नई चीज़ थी और इसने जंग को प्रसिद्धि, सामाज्य विस्तार और दूसरों को दास बनाने का ज़रिया बनाने के बजाय सुधार का ज़रिया बना दिया था। यही कारण है कि जब जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि मुसलमानों की इन लड़ाइयों में लूट-खसोट, बर्बरता, ज़ुल्म और अत्याचार नज़र नहीं आता जो जंग के साथ अनिवार्य समझा जाता है।
शाम (सीरिया) पर चढ़ाई के लिए जब पहला लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जो दस हिदायतें दीं वे जंगों की तारीख़ में मील के पत्थर की हैसियत रखती हैं। आपने हिदायत की कि किसी औरत, बूढ़े और बच्चे का क़त्ल न किया जाए, फलदार पेड़ों को न काटा जाए, आबाद जगह वीरान न की जाए, नख़लिस्तान (मरूद्यान) न जलाए जाएँ और ईसाई पादरियों को क़त्ल न किया जाए। ये हिदायतें एक बार नहीं बार-बार दी गईं और इनपर पूरी तरह अमल भी किया गया।
इस्लाम से पूर्व सिकन्दर यूनानी की जीतों, रूमियों और ईरानियों की जंगों और हूणों की चढ़ाइयों से इतिहास का हर विद्यार्थी अवगत है। इन तमाम जंगों में बेगुनाह नागरिकों का क़त्ले आम, लूटमार और औरतों की बेइज़्ज़ती आम बात थी। इस्लाम के प्रारंभ के समय ईरान और रूम के बीच कई साल तक लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा था जिसके कारण दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के इलाक़े में इतनी तबाही और बरबादी फैली कि शहर के शहर और गाँव के गाँव उजड़ गए थे। ख़िलाफ़ते राशिदा में जंगों की जीत न सिकन्दर की जीतों से कम थी और न रूमियों और हूणों की जीतों से। लेकिन इसके बाद भी ख़िलाफ़ते राशिदा की जीतें इतनी शान्ति पूर्ण थीं कि उन्हें जंगों की बजाय लुटेरों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई क़रार देना ज़्यादा सही है। कहीं क़त्ले आम नहीं हुआ, शहरों को उजाड़ा और लूटा नहीं गया और न कहीं औरतों की बेइज़्ज़ती हुई। एक बार एक शख़्स के खेतों को फ़ौज से नुक़सान हुआ तो उसने मुक़द्दमा कर दिया और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसको हर्जाना दिलाया। फ़ौज के सदाचरण का यह हाल था कि जब दमिश्क़ (Damascus) में दाख़िल हुई तो घर के छज्जों से रूमियों की औरतें उन्हें देखने के लिए जमा हो गई थीं, लेकिन किसी फ़ौजी ने उन्हें आँख उठाकर नहीं देखा। इसलिए कि क़ुरआन में ऐसे मौक़ों पर नज़रें नीची रखने की शिक्षा दी गई थी। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) कहते हैं कि जब सहाबा की फ़ौजें शाम (Syria) की सरज़मीन में दाख़िल हुईं तो शाम के ईसाई कहते थे कि मसीह के हवारियों की जो शान हम सुनते थे, ये तो उसी शान के लोग नज़र आते हैं।
अख़लाक़ (सद्व्यवहार) और तालीम (शिक्षा)
अवाम के अख़लाक़ की निगरानी भी हुकूमत के कर्त्तव्यों में से था। बलात्कार, शराब, जुआ आदि सामाजिक अपराध थे और इन अपराधों को करनेवालों को सज़ा दी जाती थी। शराब पीनेवालों को कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी और आदी शराबियों को क़ैद की सज़ा दी जाती थी। चोरी करनेवालों के हाथ काट दिए जाते थे और बलात्कार करनेवालों को संगसार (पत्थर मारना) किया जाता था या कोड़े लगाए जाते थे।
इस्लाम से पहले की शायरी में औरतों का नाम लेना और विरोधियों की बुराई कराना, जिसे 'हिजू' कहा जाता है, आम बात थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मुसलमान शायरों को इन दोनों बातों से मना कर दिया था।
हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में मदीना के लोग बहुत ख़ुशहाल हो गए और ग़ैर अरब क़ौमों से मेलजोल के कारण कुछ लोगों को कबूतरबाज़ी और ग़ुलेलबाज़ी का शौक़ हो गया था। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इन खेलों को नापसन्दीदा क़रार दिया और इनपर पाबंदी लगा दी।
इस्लामी समाज में रिश्वत सबसे घटिया अपराध माना जाता है। ख़िलाफ़ते राशिदा का दौर इस बुराई से पाक था और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ईमानदार लोगों को हाकिम बनाया जाता था और वे इस्लामी आदेशों पर अमल करना ईमान में शामिल समझते थे। हुकूमत भी हाकिमों की निगरानी करती थी। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) तो इस मामले में इतने सख़्त थे कि नौकरी के ज़माने में जो सरकारी नौकर ख़ुशहाल हो जाते थे उनसे सख़्त हिसाब लिया करते थे और इस मामले में आप बड़े-बड़े सहाबा को भी नहीं छोड़ते थे।
एक ऐसी रियासत जिसका अपना एक अलग दृष्टिकोण एवं सिद्धान्त हो, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसके कर्मचारी और प्रजा अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सचेत हों। इस चेतना को पैदा करने का एक बड़ा माध्यम शिक्षा है। इस्लाम में शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी क़रार दिया गया है। यही कारण है कि ख़िलाफ़ते राशिदा में सरकारी देख-रेख में शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। इस्लामी ख़िलाफ़त की सीमा में हर जगह क़ुरआन की शिक्षा के लिए मकतब क़ायम किए गए जिनमें पढ़ना और लिखना दोनों सिखाए जाते थे। इन मकतबों में तनख़्वाहदार शिक्षक रखे गए थे। सिर्फ़ हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में मस्जिदों की तादाद चार हज़ार से ज़्यादा हो गई थी। ये मस्जिदें, जिनमें तनख़्वाहदार इमाम और मोअज़्ज़िन रखे गए थे, बाद में धीरे-धीरे मदरसों में बदलती गईं। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सूरा बक़रा, सूरा निसा, सूरा माइदा, सूरा हज, सूरा नूर को याद करना ज़रूरी क़रार दिया था, क्योंकि अधिकतर इस्लामी आदेश इन्हीं सूरतों में हैं। इसी प्रकार हदीसों की शिक्षा में उन हदीसों पर ज़ोर दिया जाता था जो इबादत, अख़लाक़ और मामलात से सम्बन्धित हैं। शिक्षा के विकास और व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहद में सिर्फ़ कूफ़ा शहर में तीन सौ हाफ़िज़े क़ुरआन थे जो मदीना के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र था। दूसरे बड़े शिक्षा के केन्द्र मक्का, बसरा, दमिश्क़ और फ़िस्तात थे। मदीना में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा), हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु), मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) और कूफ़ा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने वक़्त के बड़े मशहूर आलिम और मुअल्लिम (शिक्षक) थे। ये आलिम क़ुरआन और हदीस के अलावा फ़िक़्ह (इस्लामी विधान), इतिहास, शब्दकोश विज्ञान, शेरो-शायरी आदि की भी शिक्षा देते थे। इन तमाम सहाबा की रिवायतों को इस्लामी ज्ञान के विस्तार के सिलसिले में आज भी बुनियादी अहमियत प्राप्त है।
ग़ुलाम और ज़िम्मी
ग़ुलामी की प्रथा से सम्बन्धित इस्लामी आदेशों की चर्चा अहदे रिसालत वाले अध्याय में की जा चुकी है। ख़िलाफ़ते राशिदा में ग़ुलामी-प्रथा के सुधार और समाप्ति के सिलसिले में कई क़दम उठाए गए। इस ज़माने में ग़ुलामों को बड़ी तादाद में आज़ाद किया गया और अंदाज़ा है कि ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में 39 हज़ार से ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद किए गए। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने विशेष रूप से ग़ुलामी-प्रथा की समाप्ति के सिलसिले में कई क़दम उठाए। हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के दौर में फ़ित्न-ए-इरतिदाद (इस्लाम-विमुख होने का फ़ित्ना) के सिलसिले में जो लोग ग़ुलाम बनाए गए थे, हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उन सबको आज़ाद कर दिया और हुक्म दिया कि अब किसी अरब को ग़ुलाम बिलकुल न बनाया जाए। ग़ैर अरब को भी ग़ुलाम बनाने के सिलसिले में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने प्रोत्साहन नहीं दिया। जब मिस्र से कुछ ग़ुलाम मदीना लाए गए तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उन्हें वापस कर दिया और मिस्र के हाकिम हज़रत अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) को उन्होंने जिन शब्दों में निर्देश दिया उसे ग़ुलामी के इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। आपने लिखा—
“इनकी माँओं ने इन्हें आज़ाद जना है और किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वह इनका यह फ़ितरी हक़ (प्राकृतिक अधिकार) छीन ले।"
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ग़ुलामों का इतना ख़याल रखते थे कि उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे। उन्होंने एक बार एक हाकिम को केवल इस जुर्म में अपदस्थ कर दिया था कि वह एक बीमार ग़ुलाम की 'अयादत' (बीमार का हाल पूछना) को नहीं गए थे। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने वज़ीफ़ा तय करते समय भी आक़ा और ग़ुलाम का फ़र्क़ मिटा दिया और ग़ुलामों का वज़ीफ़ा उनके आक़ाओं के बराबर मुक़र्रर किया। ग़ुलाम आज़ाद करना चूँकि सवाब (पूण्य) का काम था इसलिए हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे।
ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में सिर्फ़ वही लोग ग़ुलाम बनाए जा सकते थे जो जंगों में पकड़े जाते थे। उनकी हैसियत दरअसल जंगी क़ैदियों की होती थी। चूँकि उस ज़माने के हालात के तहत उन क़ैदियों का तबादला आसान न था और उन्हें सारी उम्र क़ैदी की हैसियत से रखना ग़ैर इनसानी काम होता, इसलिए उन्हें ग़ुलाम बनाकर घर और समाज का उपयोगी सदस्य बना लिया जाता था।
इस्लाम का प्रचार
ख़िलाफ़ते राशिदा की सीमा में विभिन्न नस्ल, भाषा और धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली क़ौमें आबाद थीं। ईरानवासी फ़ारसी ज़बान बोलते थे और उनका धर्म अग्निपूजा था। मिस्र और शाम (सीरिया) में क़िब्ती, सुरयानी और यूनानी ज़बानें बोली जाती थीं और उन देशों के वासी ईसाई थे। अरबी ज़बान केवल अरब और उससे लगे हुए इलाक़ो में बोली जाती थी। अरबवासी लगभग सब मुसलमान थे, लेकिन दूसरे देशों में यह हाल नहीं था। ईरान, इराक़, शाम और मिस्र में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था और यहाँ की क़ौमें अपने पैतृक धर्म को छोड़कर इस्लाम में शामिल हो रही थीं, लेकिन इन मुल्कों की बहुसंख्यक आबादी अब भी ग़ैर मुस्लिम थी। मुसलमान नागरिकों को, चाहे वे किसी मुल्क अथवा नस्ल से सम्बन्ध रखते हों, वही अधिकार प्राप्त थे जो अरब मुसलमानों को प्राप्त थे। उनका ग़ैर अरब होना अरबों के बराबर अधिकार प्राप्त करने की राह में बाधक नहीं था। परन्तु ख़िलाफ़ते राशिदा चूँकि एक सैद्धान्तिक रियासत थी और ऐसी क़ौमी हुकूमत नहीं थी, जिसकी बुनियाद वतन या नस्ल पर हो, इसलिए ग़ैर मुस्लिम आबादी को हुकूमत में बराबर की हैसियत से शामिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन आम नागरिक की हैसियत से ग़ैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। इस्लामी हुकूमत ने चूँकि उनकी उन्नति और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली थी, इसलिए उस ग़ैर मुस्लिम आबादी को ज़िम्मी कहा जाता था। ज़िम्मियों पर फ़ौजी सेवा अनिवार्य नहीं थी और इसके बदले में उनसे एक मामूली टैक्स लिया जाता था जो जिज़्या कहलाता था। ख़िलाफ़ते राशिदा में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जब मुसलमान किसी जीते हुए इलाक़े की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते थे और उस इलाक़े को ख़ाली करने को मजबूर होते थे तो जिज़्या की रक़म ग़ैर मुस्लिमों को वापस कर देते थे। जंगें हारी हुई क़ौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से ऐसे न्याय पर आधारित सुलूक की मिसाल ख़िलाफ़ते राशिदा के अलावा किसी दौर में नहीं मिलेगी। इस्लामी हुकूमत मुसलमानों की तरह ग़ैर मुस्लिमों के आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी ज़िम्मेदार थी और जो ग़ैर मुस्लिम मुहताज हो जाते थे उन्हें सरकारी बैतुलमाल से वज़ीफ़ा दिया जाता था।
अरब में नजरान के ईसाइयों और ख़ैबर के यहूदियों को कुछ कारणों से हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने देश-निकाला दे दिया था, परन्तु उन्हें नए घरों में आबाद होने की पूरी सहूलतें दी गईं। इस प्रकार कुछ जगहों की ज़िम्मी आबादी को एक विशेष प्रकार का लिबास पहनने की हिदायत दी गई थी, परन्तु उसका मक़सद उन्हें अपमानित करना नहीं था जैसा कि कुछ ग़ैर मुस्लिम इतिहासकार इलज़ाम लगाते हैं। इस्लाम में चूँकि लिबास के मामले में मुसलमानों को ग़ैर मुस्लिमों से एकरूपता पैदा करने से मना किया गया है, इसलिए इस पाबंदी का मक़सद दोनों क़ौमों की व्यक्तिगत पहचान को क़ायम रखना था, किसी को अपमानित करना या किसी को निम्न समझना इस आदेश का मक़सद नहीं था।
अरब का इनक़िलाब विश्वव्यापी बन गया
संक्षेप में ख़िलाफ़ते राशिदा की यही वे विशेषताएँ हैं जिनके कारण इस दौर की एक अलग पहचान बनी। विश्व इतिहास के अन्य दौर ऐसी विशेषताओं से ख़ाली हैं। कुछ क़ौमों के इतिहासों में इनमें से कुछ विशेषताएँ तो मिल जाएँगी, परन्तु ये तमाम विशेषताएँ एक साथ किसी क़ौम की तारीख़ में नहीं मिलेंगी। यह हक़ीक़त है कि इस दौर में मुसलमानों की तलवारों ने जितना काम किया उससे कहीं अधिक काम उनके सद्आचरणों और सद्व्यवहारों ने किया—
"उन्होंने (ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने) तबई (प्राकृतिक) क़ानूनों को शरई क़ानूनों के तहत इस्तेमाल करके ज़मीन में ख़ुदा की ख़िलाफ़त का पूरा-पूरा हक़ अदा कर दिया। उनके काल में जो संस्कृति थी उन्होंने उसके जिस्म में इस्लामी तहज़ीब (सभ्यता) की रूह फूँकी।" [ग़ैर मुस्लिमों को अपने धर्म पर अमल करने की पूरी आज़ादी थी और उनको इस्लाम क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। एक बार हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने दास को इस्लाम की दावत दी, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने यह कहकर कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं, ख़ामोशी इख़तियार कर ली।
ख़िलाफ़ते राशिदा अगरचे एक नज़रियाती (सैद्धांतिक) रियासत थी जिसका राजनीतिक और सामूहिक दृष्टिकोण इस्लाम पर आधारित था, लेकिन ग़ैर मुस्लिम जनता को इस दृष्टिकोण से विरोध करने की आज्ञा थी, हालांकि शैक्षणिक व्यवस्था में भी ग़ैर मुस्लिमों को इस्लामी अक़ीदे की शिक्षा प्राप्त करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था।]
किसी क़ौम की तारीख़ में तीस साल की अवधि बहुत कम होती है। परन्तु ठोस कारनामों को सामने रखा जाए तो ख़िलाफ़ते राशिदा के ये तीस साल दूसरी क़ौमों के सैकड़ों सालों के इतिहास पर भारी हैं। इस अल्प अवधि में एक मामूली रियासत जो अरब प्रायद्वीप तक सीमित थी, दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत बन गई। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दौर में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन अरब और अरबों की ज़िन्दगी में हुआ था वैसा ही परिवर्तन ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में ईरान, इराक़, शाम और मिस्र में और उन मुल्कों में आबाद क़ौमों में आया।
ईरानी और रूमी उस ज़माने में दुनिया की सबसे सभ्य और शक्तिशाली क़ौमों में गिने जाते थे। इराक़, शाम और मिस्र वे मुल्क थे, जहाँ इनसान ने सबसे पहले सभ्यता का पाठ पढ़ा था और जिसके कारण उस क्षेत्र को सभ्यता का केन्द्र कहा जाता है। तीस साल की इस अल्प अवधि में उन तमाम प्रचीन क़ौमों की राजनीतिक शक्ति ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सभ्यता के मैदान में भी उन्हें हार माननी पड़ी। उन्होंने तेज़ी से अपने पुराने धर्म को छोड़कर इस्लाम क़बूल करना शुरू किया कि आगामी पचास-साठ साल की अवधि में उन मुल्कों की लगभग सारी आबादी मुसलमान हो गई और ये मुल्क हमेशा के लिए इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गए। धर्म के साथ ही इन क़ौमों का जीवन से सम्बन्धित दृष्टिकोण भी बदल गया और इस प्रकार एक नई सभ्यता की बुनियाद पड़ी जो स्थानीय विशेषताओं के बावजूद इस्लामी सभ्यता कहलाई और जिसके चिह्न चौदह सौ साल बाद आज भी बाक़ी हैं। मुसलमानों की यह महान सफलता तलवार का नतीजा नहीं थी, बल्कि इस्लाम की श्रेष्ठ एवं उच्च शिक्षाओं और मुसलमानों के सद्व्यवहार और सदाचरणों का नतीजा थी।
दुनिया की विभिन्न क़ौमों और गिरोहों के सामने कोई न कोई आदर्श लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह जिद्दोजुहद (संघर्ष) करती है। परन्तु अभी तक राजनीतिक और सामूहिक मैदान में कोई ऐसा आदर्श लक्ष्य नज़र नहीं आता जिसे प्राप्त कर लिया गया हो। हर लक्ष्य भविष्य की एक आरज़ू ही है। परन्तु यह विशेषता सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम और इस्लाम के इतिहास की है कि ख़िलाफ़ते राशिदा के रूप में एक आदर्श राजनीतिक और सामूहिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। यही कारण है कि ख़िलाफ़ते राशिदा का दौरे हुकूमत अपने सकारात्मक और ठोस कारनामों और अपनी अलग ख़ूबियों के कारण आनेवाली नस्लों के लिए एक आदर्श एवं अनुकरणीय नमूना बन गया। आज भी इस्लामी दुनिया में उसकी यह हैसियत बरक़रार है। हम अगले पृष्ठों में देखेंगे कि जो हुकूमत अपनी विशेषताओं में ख़िलाफ़ते राशिदा के जितना ज़्यादा अनुरूप और निकट थी उतना ही उसमें कम ख़राबियाँ नज़र आती हैं और जो हुकूमत जितनी ज़्यादा उससे भिन्न थी, उसमें उतनी ही ज़्यादा ख़राबियाँ नज़र आती हैं।
अध्याय-8
पूरब और पश्चिम की फ़तह
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु)
हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़िलाफ़त से हटने के बाद अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुसलमानों की आम सहमति से ख़लीफ़ा स्वीकार कर लिए गए, परन्तु वह मुसलमानों के चुने हुए ख़लीफ़ा नहीं थे, बल्कि उन्होंने ताक़त के ज़ोर से ख़िलाफ़त हासिल की थी। जब वह ख़लीफ़ा बन गए तो लोगों ने मजबूरन बैअत कर ली, क्योंकि यदि वे बैअत न भी करते तो भी अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ख़िलाफ़त से दस्तबरदार नहीं होते और ख़ानाजंगी (गृह युद्ध) जारी रहती। इस प्रकार ख़िलाफ़ते राशिदा की चुनाव प्रणाली ख़त्म हो गई और इस्लामी इतिहास में मुलूकियत (बादशाहत) का आगाज़ हुआ।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बैअत हो जाने के बाद जब मशहूर सहाबी हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) उनसे मिले तो उन्होंने अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को "ऐ बादशाह! अस्सलामु अलैकुम!" कहकर ख़िताब किया, हालाँकि अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अमीरुल-मोमिनीन के बजाए बादशाह कहकर पुकारा जाना बुरा लगा, परन्तु उन्हें ख़ुद भी इस हक़ीक़त की जानकारी थी कि वे मुसलमानों में पहले बादशाह हैं।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जिस हुकूमत की बुनियाद डाली उसे 'ख़िलाफ़त बनी उमय्या' या 'उमवी ख़िलाफ़त' कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस हुकूमत में जितने ख़लीफ़ा हुए वे सब "उमय्या" के ख़ानदान से थे। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बीस साल हुकूमत की। उनके ज़माने में पूरी सल्तनत में सुख-शान्ति रही। नए-नए इलाक़ों पर विजय भी मिली। उन नए इलाक़ों में एक उत्तरी अफ़्रीक़ा है। उत्तरी अफ़्रीक़ा को उस ज़माने के मशहूर सिपहसालार 'उक़बा बिन नाफ़े' ने फ़तह किया। उक़बा बिन नाफ़े बड़े उत्साही सिपहसालार थे। जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो कई सौ मील तक इलाक़े पर इलाक़े फ़तह करते चले गए, यहाँ तक कि समुद्र सामने आ गया। यह अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean) था जिसे Black Sea भी कहा जाता है। उक़बा ने जब देखा कि समुद्र उनके मार्ग में है तो उन्होंने अपना घोड़ा समुद्र में दौड़ा दिया और जोश में दूर तक चले गए फिर तलवार उठाकर कहा कि ऐ ख़ुदा! अगर यह समुद्र बाधक न होता तो मैं दुनिया के आख़िरी किनारे तक तेरा नाम बुलन्द करता हुआ चला जाता।
उत्तरी अफ़्रीक़ा चूँकि इस्लामी दुनिया से काफ़ी दूर था इसलिए उक़बा ने वहाँ 'कैरवान' (Kairwan) के नाम से एक शहर बसाया ताकि उस क्षेत्र में मुसलमान स्थायी रूप से रह सकें। यह शहर बाद में कई सौ वर्ष तक इस्लामी सभ्यता, ज्ञान और कला का बड़ा केन्द्र रहा। उक़बा बड़े नेक बुज़ुर्ग थे। उनका मज़ार उत्तरी अफ़्रीक़ा में 'बस्करह' नामक बस्ती में अब भी मौजूद है और हज़ारों लोग उसका दर्शन करने जाते हैं।
हालाँकि अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) सहाबी थे पर उन्हें अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की संगत में रहने का बहुत कम अवसर मिला था। वे फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे, इसलिए सिर्फ़ तीन साल आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की संगत में रह सके। इसके कारण उनके अन्दर वह ख़ूबी पैदा नहीं हो सकी जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में या उन सहाबियों में थी जिन्हें अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ख़िदमत करने का ज़्यादा मौक़ा मिला था। वे अपनी हुकूमत क़ायम करने के लिए हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से लड़े। अपने बाद अपने बेटे यज़ीद को ख़लीफ़ा बनाया। वे ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सादा ज़िंदगी के बजाए शाहाना ज़िन्दगी गुज़ारते थे और मुसलमानों के बैतुलमाल से अपनी मरज़ी के मुताबिक़ ख़र्च करते थे। उनके दरबार का अंदाज़ शाहाना था। वह बादशाहों की तरह तख़्त पर बैठते थे, जिसके पाए सोने के होते थे। वे जब बाहर निकलते थे तो आगे-आगे चोबदार चलते थे। वह पहले ख़लीफ़ा थे जिन्होंने अपने लिए चोबदार और पहरेदार (बॉडीगार्ड) मुक़र्रर किए। उन्हें शानदार महल बनाने का शौक़ था और उन महलों के बारे में दूसरों की राय मालूम करते थे। शुरू में हालाँकि उनका महल शानदार था, लेकिन उसके निर्माण में मिट्टी का प्रयोग किया गया था। एक बार रूम से एक प्रतिनिधि आया। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उससे अपने महल के बारे में राय ली। प्रतिनिधि ने कहा, "इसका ऊपर का हिस्सा चिड़ियों के लिए है और नीचे का चूहों के लिए।"
अतः अमीर मुआविया ने इसके बाद महलों के निर्माण में मिट्टी की बजाय पत्थर इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे ही किसी महल के बारे में एक बार हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से राय तलब की तो उन्होंने अपने नेक वालिद की तरह दो टूक जवाब दिया—
"यदि आपने यह महल बैतुलमाल के धन से बनाया है तो मुसलमानों के साथ ख़ियानत (धोखा) किया है और यदि अपने निजी धन से बनाया है तो फ़ुज़ूलख़र्ची की है।"
ये थे इन महलों के निर्माण से सम्बंधित दो भिन्न दृष्टिकोण। उनमें एक बादशाहत का दृष्टिकोण था और दूसरा ख़िलाफ़त का और बहुत हद तक अवाम का। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को कुछ तो नई परिस्थितियों के कारण और कुछ व्यक्तिगत रुझान के कारण पहला दृष्टिकोण पसन्द आया था। लेकिन इसके बावजूद अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) बहुत अच्छे हुक्मराँ थे। इतने अच्छे कि बाद में उन जैसे हुक्मराँ इस्लामी इतिहास में कम हुए।
वह किसी काम के लिए जनता की आम सहमति के पाबंद नहीं थे, परन्तु कुछ न कुछ उसका लिहाज़ रखते थे और ज़्यादा कट्टर भी नहीं थे। उन्होंने अपने शासन के उसूल इस प्रकार बयान किए हैं—
"जहाँ मेरा कोड़ा काम देता है, वहाँ तलवार काम में नहीं लाता और जहाँ मेरी ज़बान काम देती है, वहाँ कोड़ा काम में नहीं लाता। यदि मेरे और लोगों के बीच बाल बराबर भी रिश्ता क़ायम हो तो मैं उसे नहीं तोड़ता। जब लोग उसे खींचते हैं तो मैं ढील दे देता हूँ और जब वे ढील देते हैं तो मैं खीच लेता हूँ।" —तारीख़े इस्लाम, भाग-II, पृ०-37, शाह मुईनुद्दीन अहमद नदवी
वे बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में बड़े योग्य हाकिम मुक़र्रर किए थे जिनके कारण बीस साल तक उन्होंने शान्तिपूर्वक शासन किया। उनके ज़माने में ऐसा अम्न था कि इराक़ का हाकिम ज़ियाद कहता था, “यदि कूफ़ा और ख़ुरासान के रास्ते में रस्सी का एक टुकड़ा भी खो जाए तो मुझे मालूम हो जाएगा कि किसने लिया।” रातों को औरतें अपने घरों में किवाड़ खोलकर अकेली सोती थीं।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) का स्वभाव इतना अच्छा था कि वे किसी के साथ कठोरता से पेश नहीं आते थे, लोग उन्हें उनके मुँह पर भी बुरा-भला कह जाते थे। वे अपने विरोधियों को भी इनाम और सम्मान देकर ख़ुश रखते थे। हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके ख़ानदानवालों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और उनकी लाखों रुपये से मदद करते थे।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जनकल्याण के बहुत काम हुए। नहरें खोदी गईं और सिंचाई के लिए तालाब बनाए गए।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) पहले ख़लीफ़ा हैं जिन्होंने डाक का इंतिज़ाम किया। इसका तरीक़ा यह था कि मुल्क भर में थोड़े-थोड़े फ़ासले पर तेज़रफ़्तार घोड़े हर समय तैयार रहते थे। सरकारी कारिंदे हर मंज़िल पर उन घोड़ों को बदलते हुए एक स्थान की ख़बरें दूसरे स्थान तक लाते और ले जाते थे।
यदि हम अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को एक बादशाह की हैसियत से देखें तो उनके दौर में हमें ख़ामियाँ कम और ख़ूबियाँ ज़्यादा नज़र आएँगी। उनके दौर की ख़ामियाँ बादशाही शासन प्रणाली की स्वभाविक ख़ामियाँ हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत ख़ामियाँ नहीं हैं।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने शाम (सीरिया) के शहर दमिश्क़ को राजधानी बनाया, जहाँ वह ख़िलाफ़त से पहले कई साल से गवर्नर की हैसियत से रहते चले आ रहे थे। यह शहर मदीना और कूफ़ा के बाद इस्लामी ख़िलाफ़त की तीसरी राजधानी था। दमिश्क़ सभ्यता एवं संस्कृति का प्राचीन केन्द्र था, इसलिए इस्लामी रियासत के भविष्य के निर्माण में इसकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता।
ख़ानाजंगी (गृह युद्ध) और करबला का वाक़िआ
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने बाद अपने लड़के यज़ीद (60 हि०/680 ई० से 64 हि०/684 ई०) को अपना जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर किया। ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में ख़लीफ़ा का चुनाव मशविरे से किया जाता था और कभी किसी ख़लीफ़ा ने अपने बेटे को ख़लीफ़ा नहीं बनाया था। मुसलमानों का मानना था कि हुकूमत घर की तरह किसी एक की जायदाद नहीं होती है, जिसका बाप के बाद बेटा उत्तराधिकारी बने। हुकूमत तो नगर एवं देश की व्यवस्था बनाने के लिए क़ायम की जाती है और एक प्रकार की सेवा है। प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का मशहूर कथन है, "क़ौम का सरदार उसका ख़ादिम (सेवक) होता है।" इसलिए सरदारी का यह काम योग्य आदमी के सुपुर्द होना चाहिए, लेकिन अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने ज़माने के बड़े-बड़े योग्य लोगों को नज़रअंदाज़ करके अपने लड़के यज़ीद को, जो बहुत-सी बातों में बदनाम था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसमें शक नहीं कि अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इस मसले पर कई लोगों से मशविरा कर लिया था और यज़ीद की बैअत हज के मौक़े पर हज़ारों लोगों ने की थी। परन्तु यह बैअत दबाव के तहत की गई थी। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) हर हाल में अपने बेटे को ख़लीफ़ा बनाना चाहते थे और यदि लोग बैअत न करते तो वह अपने इस इरादे से पीछे न हटते। यज़ीद की जानशीनी (उत्तराधिकारी होने) का जिन पाँच बड़े सहाबा ने खुलकर विरोध किया उनके नाम ये हैं :
हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु)। इनमें हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने तो अमीर-मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) से साफ़-साफ़ कह दिया था कि अपने बेटे को जानशीन बनाना अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का तरीक़ा नहीं है, बल्कि क़ैसर व किसरा का तरीक़ा है।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उन लोगों का मशविरा नहीं माना और अपने बेटे को जानशीन मुक़र्रर करके इस्लाम के इतिहास में एक ग़लत राजनीतिक परम्परा की बुनियाद डाली जिसने मुलूकियत (राजतंत्र) को और मज़बूती प्रदान की।
मौजूदा दौर के एक महान अंवेषक ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—
"इसके बाद मुलूकियत का यह निज़ाम ऐसा मज़बूत हुआ कि मौजूदा सदी में मुस्तफ़ा कमाल के अलफ़ाए ख़िलाफ़त तक एक दिन के लिए भी उसमें गड़बड़ी न हुई। ज़ोर-ज़बरदस्ती बैअत और ख़ानदानों की मौरूसी बादशाहत का एक मुस्तक़िल तरीक़ा चल पड़ा। लोग मुसलमानों के आज़ादाना और खुले मशविरे से नहीं बल्कि ताक़त के ज़ोर पर हुकूमत में आते रहे। बैअत से हुकूमत हासिल करने के बजाय ताक़त से बैअत हासिल होने लगी। बैअत का हासिल होना हुकूमत पर क़ाबिज़ होने और क़ाबिज़ रहने के लिए शर्त न रहा। लोगों की पहले तो यह मजाल न थी कि जिसके हाथ में सत्ता आई हुई थी, उसके हाथ पर बैअत न करते लेकिन अगर वे बैअत न भी करते तो उसका नतीजा कभी भी यह न होता कि जिसके हाथ में सत्ता आ गई हो वह उनकी बैअत न करने की वजह से रह जाए।" —ख़िलाफ़त व मलूतकयत : मौलाना मौदूदी, पृ० 159
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इंतिक़ाल के बाद जब यज़ीद ख़लीफ़ा हुआ तो बहुत-से लोगों ने विरोध प्रकट किया। इस विरोध का एक कारण यह था कि वे जानशीन के इस तरीक़े को क़ैसर (रूम का बादशाह) व किसरा (ईरान का बादशाह) का तरीक़ा समझते थे, इस्लामी तरीक़ा नहीं समझते थे। और दूसरा कारण यह था कि वे यज़ीद को व्यवहार और आचरण की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं समझते थे कि उसे मुसलमानों का ख़लीफ़ा बनाया जाए। उन विरोध करनेवालों में प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नवासे यानी आपकी बेटी फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के बेटे हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी थे।
इराक़ में कूफ़ा के लोगों ने हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) का साथ देने का वादा किया और उन्हें कूफ़ा आने की दावत दी। इस मौक़े पर कुछ सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने आपको कूफ़ा जाने से रोकना चाहा। उनमें से एक आपके भाई मुहम्मद बिन हनफ़िया भी थे। [मुहम्मद बिन हनफ़िया हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के सौतेले भाई थे। वे हज़रत फ़ातिमा से नहीं बल्कि हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की दूसरी बीवी से पैदा हुए थे।] उन्होंने हज़रत हुसैन से कहा कि आप अपने आदमी को भेजकर कूफ़ा के लोगों को अपनी ख़िलाफ़त की दावत दीजिए। अगर वे बैअत कर लें तो हमारे लिए यह बेहतर होगा और अगर आपके अलावा किसी और शख़्स पर मुसलमानों की आम सहमति हो जाए तो इससे मज़हब और आपकी बुज़ुर्गी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परन्तु हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इन मशविरों को नज़रअंदाज़ कर दिया और कूफ़ावालों की दावत पर अपने ख़ानदान के 72 आदमियों को साथ लेकर जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, मक्का से कूफ़ा रवाना हो गए। परन्तु इस दौरान यज़ीद का नियुक्त किया हुआ हाकिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफ़ा पहुँच गया और कूफ़ा के लोग उससे डरकर न सिर्फ़ हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से किए हुए वादों से फिर गए, बल्कि हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के प्रतिनिधि और भाई मुस्लिम बिन अक़ील को जो इमाम हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पहले ही कूफ़ा पहुँच चुके थे, इब्ने ज़ियाद के सुपुर्द कर दिया। उसने उन्हें क़त्ल करवा दिया। कूफ़ावालों की इस बेवफ़ाई से मायूस होकर हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने वापस मक्का लौट जाना चाहा, लेकिन हज़रत मुस्लिम के भाइयों के आग्रह पर आपने सफ़र जारी रखा। इब्ने ज़ियाद के चार हज़ार आदमियों ने फ़ुरात नदी के किनारे करबला नामक स्थान पर इस क़ाफ़िले को घेर लिया और हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) को यज़ीद की बैअत करने पर मजबूर किया। उन्होंने इब्ने ज़ियाद के आदमियों से कहा कि या तो हमें यज़ीद के पास जाने दो या फिर सरहद की ओर जाने दो, ताकि हम इस्लाम विरोधियों से जिहाद कर सकें या हमें वापस मदीना जाने दो। परन्तु इब्ने ज़ियाद ने उनकी कोई शर्त मंज़ूर नहीं की और यज़ीद की बैअत पर मजबूर किया। परन्तु हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) ऐसे इनसान नहीं थे जो मौत से डरकर और दबाव में आकर कोई बात क़बूल कर लेते। उन्होंने जान देना क़बूल कर लिया, लेकिन ज़ोर-ज़बरदस्ती के आगे झुकना पसंद नहीं किया। मुक़ाबला बेजोड़ था। थोड़े-से लोग चार हज़ार लोगों का मुक़ाबला नहीं कर सकते थे। नतीजा यह हुआ कि हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके क़ाफ़िले के तमाम मर्द शहीद हो गए। मर्दों में सिर्फ़ उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन बचे जो बीमार होने के कारण जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) का सिर काट कर यज़ीद के पास दमिश्क़ भिजवा दिया। उनके क़ाफ़िले के बचे-खुचे लोगों में सिर्फ़ औरतें और बच्चे थे, उनको भी यज़ीद के पास रवाना कर दिया।
करबला का यह वाक़िआ इस्लामी इतिहास का बड़ा अफ़सोसनाक हादसा है। इसके ज़िम्मेदार यज़ीद हों या इब्ने ज़ियाद, मुसलमानों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नवासे से ऐसा सुलूक करेंगे। अतः करबला के इस वाक़िआ की अरब में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और मक्का एवं मदीना के लोगों ने यज़ीद की बैअत तोड़कर मशहूर सहाबी हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हाथ पर ख़िलाफ़त की बैअत कर ली। यज़ीद ने इस असन्तोष को दबाने के लिए मदीना की ओर फ़ौज भेजी, जिसने मदीना फ़तह करने के बाद शहर में क़त्ले आम किया और तीन दिन तक शहर में लूटमार की। यह भी इस्लामी इतिहास पर एक काला धब्बा है, क्योंकि मुसलमानों ने अभी तक आम नागरिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया था। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बीच चार साल तक जंग जारी रही, लेकिन कभी किसी ने दूसरे के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जो मानवता के विरुद्ध हो। यज़ीद की भेजी हुई फौज़ ने मदीना के बाद मक्का की ओर कूच किया जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) मौजूद थे। परन्तु इस बीच यज़ीद की मृत्यु हो गई और उसके आदमी वापस दमिश्क़ चले गए।
यज़ीद की मृत्यु के बाद अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई, क्योंकि यज़ीद के बेटे ने हुकूमत क़बूल करने से इनकार कर दिया। कोई ख़लीफ़ा न होने के कारण इस्लामी दुनिया में बिखराव आने लगा। मुसलमानों की नज़रें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) पर पड़ीं और उन्होंने उनके हाथ पर बैअत कर ली। इस प्रकार मिस्र, शाम (सीरिया), इराक़ बल्कि पूरी इस्लामी ख़िलाफ़त हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हाथ में आ गई। परन्तु शाम (सीरिया) में एक स्थान पर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के समर्थकों और बनी उमय्या के समर्थकों के बीच घमासान का युद्ध हुआ, जिसमें बनी उमय्या सफ़ल रहे और शाम (सीरिया) से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सत्ता समाप्त हो गई। बाक़ी इस्लामी दुनिया पर उनकी सत्ता सात साल तक क़ायम रही। परन्तु इस दौरान में बनी उमय्या के समर्थक ज़ोर पकड़ते गए, यहाँ तक कि एक उमवी हुक्मराँ अब्दुल मलिक इस संघर्ष में कामयाब हो गया और मक्का पर भी उसका क़ब्ज़ा हो गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) उसके एक सिपहसालार हज्जाज बिन यूसुफ़ के मुक़ाबले में जंग करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद ख़िलाफ़त शासन-प्रणाली की रही-सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई।
अब्दुल मलिक (65 हि०/685 ई० से 86 हि०/705 ई०)
यज़ीद के बाद जो लोग ख़लीफ़ा हुए वे अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में से नहीं थे, लेकिन वे भी अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की तरह ख़ानदान बनी उमय्या से सम्बन्ध रखते थे। इस नए ख़ानदान का बानी (संस्थापक) 'मरवान बिन हकम' था जो एक ज़माने में हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) का सेक्रेट्री था। हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की समस्याओं का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार यही व्यक्ति था। जब मदीना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हुकूमत क़ायम हो गई तो मरवान शाम (सीरिया) चला गया जहाँ 64 हि०/684 ई० में बनी उमय्या के समर्थकों ने उसे ख़लीफ़ा बना दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से जंग के बाद शाम (सीरिया) और मिस्र पर उसका क़ब्ज़ा हो गया। परन्तु वह सिर्फ़ नौ माह ख़िलाफ़त कर के रमज़ान 65 हि०/685 ई० में मर गया और उसकी जगह उसका लड़का अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा हुआ।
अब्दुल मलिक 39 साल की उम्र में तख़्त पर बैठा। वह मदीने के बड़े आलिमों (विद्वानों) में गिना जाता था। वह बड़ा साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को पराजित कर के पूरी इस्लामी रियासत का हुक्मराँ बन गया। उसे प्रारंभ में कई बग़ावतों का समाना करना पड़ा। उनमें ख़ारजियों की बग़ावत जिसके केन्द्र इराक़ और ईरान थे, सबसे अधिक ख़तरनाक थी। ये बग़ावत कई साल जारी रही और अन्ततः मुहल्लब बिन अबी सफ़रह की कोशिशों से, जो अपने वक़्त का सबसे बड़ा सिपहसालार था, ये बग़ावतें कुचल दी गईं और पूरी सल्तनत में शान्ति हो गई। अपने इन कारनामों के कारण अब्दुल मलिक ख़ानदान बनी उमय्या का बानी (संस्थापक) समझा जाता है। हालाँकि उत्तरी अफ़्रीक़ा अमीर मुआविया के काल में ही इस्लामी ख़िलाफ़त का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वहाँ के बर्बरवासी बार-बार बाग़ी हो जाते थे। अब्दुल मलिक के अहद में उत्तरी अफ़्रीक़ा को दोबारा फ़तह किया गया। यह काम एक सिपहसालार 'मूसा बिन नसीर' ने अंजाम दिया, जो 79 हि०/698 ई० में उत्तरी अफ़्रीक़ा के हाकिम बनाए गए थे। मूसा ने न केवल जंगी कामयाबी हासिल की, बल्कि उन्होंने बर्बरियों में इस्लाम की तबलीग़ (प्रचार) भी की। उनके अहद में पूरा उत्तरी अफ़्रीक़ा मुसलमान हो गया और इस प्रकार बर्बर क़ौम इस्लामी ख़िलाफ़त के शान्तिप्रिय नागरिक बन गए। मूसा बिन नसीर ने समुद्री फ़ौज को भी तरक़्क़ी दी और इस उद्देश्य के लिए तूनिस (Tunish) में जहाज़ बनाने का कारख़ाना स्थापित किया। अब्दुल मलिक के अहद का एक और कारनामा 'क़ुब्बतुस-सख़रा' की तामीर (निर्माण) है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बैतुल-मक़्दिस मुसलमानों का पहला क़िबला (वह दिशा जिधर मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं) था और यहीं से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेराज के मौक़े पर आसमान पर गए थे, लेकिन वह ख़ास जगह जहाँ से हुज़ूर ऊपर गए थे, एक चट्टान थी, जो मस्जिदे अक़सा की परिधि के अन्दर थी। अब्दुल मलिक ने उस चट्टान के ऊपर एक आलीशान गुम्बद बनवा दिया जो अब तक मौजूद है और कला एवं शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना समझा जाता है। अरबी में चट्टान को सख़रा कहा जाता है, इसलिए यह गुम्बद 'क़ुब्बतुस-सख़रा' कहलाता है।
कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि अब्दुल मलिक ने क़ुब्बतुस-सख़रा इसलिए तामीर किया था कि मुसलमान ख़ान-ए-काबा के बदले इसका तवाफ़ (परिक्रमा) किया करें। यह बिलकुल झूठा इल्ज़ाम है। अब्दुल मलिक ख़ुद एक सच्चा मुसलमान था और यदि ऐसा न भी होता तो वह ऐसा साहस नहीं कर सकता था। मुसलमान अवाम जिनका नेतृत्व आलिमों के हाथ में था, उसके ख़िलाफ़ बग़ावत कर देते। उमवी हुक्मरानों पर ऐसे इल्ज़ाम उन इतिहासकारों ने लगाए हैं जो उमवी ख़ानदान के विरोधी थे। अब्दुल मलिक ने क़ुब्बतुस-सख़रा दरअसल बैतुल मक़्दिस की ईसाई इमारतों के मुक़ाबले में तामीर किया था।
अब्दुल मलिक का ज़माना दो बातों के कारण बड़ा मशहूर है। एक दफ़्तरों की ज़बान अरबी करना और दूसरा सिक्कों का ढालना। अब्दुल मलिक के ज़माने तक दफ़्तरों का काम स्थानीय ज़बान में होता था। उसने यह अरबी में करने का हुक्म दिया। इसी प्रकार अब तक इस्लामी रियासत में ग़ैर मुल्की सिक्के चलते थे। हालाँकि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से इस्लामी सिक्के बनने लगे थे, लेकिन ये सिक्के बहुत कम होते थे, इसलिए इस्लामी रियासत में रूमी सिक्के का ज़्यादा प्रचलन था। अब्दुल मलिक के ज़माने में रूमी बादशाह ने यह धमकी दी कि वह रूमी सिक्कों पर पैग़म्बरे इस्लाम को गालियाँ लिखवाएगा। जब अब्दुल मलिक को यह मालूम हुआ तो उसने रूमी सिक्कों का दाख़िला बंद कर दिया और दमिश्क़ और कूफ़ा में बड़ी-बड़ी टक्सालें क़ायम कीं जहाँ रोज़ाना लाखों सिक्के ढलकर तैयार होने लगे।
वलीद बिन अब्दुल मलिक (86 हि०/705 ई० से 96 हि०/715 ई०)
(1)
अब्दुल मलिक के बेटे वलीद का ज़माना जंगों में जीत के कारण मशहूर है। इस ज़माने में जितनी जंगें जीती गईं उनका हाल पढ़कर हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने की याद आती है।
ईरान की ओर इस्लामी ख़िलाफ़त की सीमा जैहून नदी तक थी। वलीद के सिपहसालार क़ुतैबा ने बुख़ारा, समरक़ंद, ख़ीवा और काशग़र पर विजय प्राप्त कर इस्लामी हुकूमत की हद चीन की सल्तनत तक बढ़ा दी।
क़ुतैबा जब काशग़र फ़तह करके चीन की सरहद के क़रीब पहुँच गए तो उन्होंने चीन के बादशाह के सामने दो शर्तें रखीं। या तो इस्लाम लाओ या फिर जिज़्या दो। क़ुतैबा ने चीन के बादशाह के पास जो प्रतिनिधि मंडल भेजा उसने बादशाह से यह भी कहा कि हमारे सरदार ने क़सम खाई है कि मैं उस वक़्त तक वापस न जाऊँगा जब तक तुम्हारी ज़मीन को अपने पाँव से न रौंदूँ और मंत्रियों की गर्दन न दबाऊँ और तुमसे ख़िराज वसूल न करूँ।
बादशाह ने कहा अच्छा हम उसकी क़सम पूरी कर देते हैं और वह इस प्रकार कि अपने देश की कुछ मिट्टी उसके पास भेज देते हैं कि वह उसे रौंदे। कुछ शहज़ादे भेजते हैं कि वह उनकी गर्दनों को नीचा करे और इतना जिज़िया देते हैं कि जिससे वह ख़ुश हो जाए।
चीन के बादशाह ने उसके बाद चार शहज़ादे और मिट्टी क़ुतैबा के पास भिजवा दी, जिससे वह ख़ुश हो गए। इधर चीन के बादशाह ने यह चालाकी की, उधर ख़लीफ़ा वलीद का इंतिक़ाल हो गया और नए ख़लीफ़ा ने क़ुतैबा को वापस आने का हुक्म भेज दिया, जिसके कारण चीन का मुल्क फ़तह नहीं हो सका।
(2)
भारत में मुसलमानों का प्रवेश भी उसी काल में हुआ। इसका वाक़िआ यूँ है कि लंका के राजा ने ख़लीफ़ा को एक जहाज़ में तोहफ़े भेजे थे। इस जहाज़ में बहुत-से मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे भी थे जो लंका से अरब जा रहे थे। जब यह जहाज़ सिन्ध के समुद्री तट के निकट से गुज़रा तो यहाँ के समुद्री डाकुओं ने उसे लूट लिया और मुसलमान औरतों और बच्चों को क़ैद कर लिया। ख़लीफ़ा ने जब यहाँ के राजा को लिखा कि मुसलमानों और उनके माल को वापस कर दे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस अब क्या था, मुसलमान कोई कमज़ोर तो थे नहीं जो यह ज़ुल्म सहते। ख़लीफ़ा के हुक्म से मुहम्मद बिन क़ासिम को सिपहसालार बनाकर एक फ़ौज सिंध रवाना कर दी गई। मुहम्मद बिन क़ासिम की उम्र इस समय केवल सतरह साल थी परन्तु इतनी कम उम्र में वह इतना बुद्धिमान और वीर था कि एक पूरी फ़ौज का उसे सरदार बना दिया गया। उस ज़माने में बलूचिस्तान, सिंध और मुलतान का इलाक़ा सिंध की हुकूमत में था और यहाँ के राजा का नाम दाहिर था। मुहम्मद बिन क़ासिम बलूचिस्तान के रास्ते से आया और सबसे पहले दैबल की बन्दरगाह को फ़तह किया जो कराँची के मौजूदा शहर से क़रीब किसी जगह स्थित था। यहाँ मुहम्मद बिन क़ासिम ने ये तमाम क़ैदी रिहा करा लिए जिन्हें डाकुओं ने गिरफ़्तार कर लिया था। इसके बाद मुहम्मद बिन क़ासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर लड़ाई में मारा गया।
यह जंग रावर नामक स्थान पर हुई थी जो दक्षिणी सिंध में किसी जगह था। यह एक बड़ी जंग थी जिसने फ़ैसला कर दिया कि भारत का यह पश्चिमी भाग (जो पाकिस्तान बन चुका है) आइंदा इस्लामी दुनिया का हिस्सा होगा। मुहम्मद बिन क़ासिम ने पूरा सिंध प्रांत और मुलतान फ़तह कर लिया। मुहम्मद बिन क़ासिम अब उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहता था, जहाँ कन्नौज के राजा का शासन था। परन्तु इस बीच वलीद का इंतिक़ाल हो गया और नए ख़लीफ़ा ने मुहम्मद बिन क़ासिम को वापस बुला लिया जिसके कारण चीन की तरह भारत पर भी मुसलमानों का क़बज़ा नहीं हो सका।
(3)
वलीद के ज़माने में तीसरी चढ़ाई पश्चिम में स्पेन और पुर्तगाल पर की गई। दोनों देश उस ज़माने में एक ईसाई बादशाह के क़बज़े में थे और उन दोनों मुल्कों को मुसलमान अपने ज़माने में 'अंदलुस' (Andlus) कहा करते थे।
अंदलुस के एक ईसाई सरदार ने वहाँ के बादशाह रॉड्रिक के अत्याचार के ख़िलाफ़ मूसा बिन नुसैर से मदद माँगी। मूसा बिन नुसैर अब्दुल मलिक के ज़माने से उत्तरी अफ़्रीक़ा के हाकिम थे। मूसा ने ख़लीफ़ा वलीद से इजाज़त लेने के बाद अपने एक बर्बर ग़ुलाम तारिक़ बिन ज़ियाद को अंदलुस की ओर भेजा। तारिक़ ने वादी-लका की जंग में बारह हज़ार फ़ौज से रॉड्रिक की एक लाख फ़ौज को पराजित किया। रॉड्रिक जंग में मारा गया। उसके बाद मूसा भी अंदलुस आ गए और मूसा और तारिक़ ने मिलकर थोड़े ही समय में न केवल पूरा अंदलुस फ़तह कर लिया, बल्कि वे पेरेनीज़ पहाड़ को पार करके फ़्रांस की सीमा में भी प्रवेश कर गए। यहाँ से ये दोनों सिपहसालार इटली, बलक़ान और क़ुस्तनतीनिया को फ़तह करते हुए शाम (सीरिया) जाना चाहते थे। लेकिन ख़लीफ़ा वलीद ने इस ख़तरनाक मुहिम की इजाज़त नहीं दी। यदि मुसलमान इस मुहिम में कामयाब हो जाते तो आज पूरा यूरोप मुसलमान होता।
हक़ीक़त यह है कि वलीद का दौर बड़े बहादुर सरदारों का दौर था। उन सिपहसालारों यानी क़ुतैबा, मुहम्मद बिन क़ासिम और मूसा बिन नुसैर को अपनी योजनाओं को स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा करने का मौक़ा मिलता तो शायद आज दुनिया का नक़्शा कुछ और ही होता।
इन बड़ी जीतों के अलावा वलीद के ज़माने में मुसलमानों को और भी कई कामयाबियाँ हासिल हुईं। एशिया-ए-कोचक के मोर्चे पर रूमियों से लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं और मुसलमानों ने उनसे कई इलाक़े छीन लिए। इन लड़ाइयों में वलीद के भाई मुसलिमा बिन अब्दुल मलिक ने सिपहसालार की हैसियत से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की।
इस दौर में कई समुद्री लड़ाइयाँ भी हुईं और मुसलमानों ने पश्चिमी रूम सागर में बिलयार्क टापुओं पर क़बज़ा कर लिया।
इन जीतों के कारण जो केवल दस साल की छोटी-सी मुद्दत में हुईं, इस्लामी हुकूमत का काफ़ी उत्थान हुआ। अब तक दुनिया में इतनी बड़ी सल्तनत पहले कभी क़ायम नहीं हुई थी। काशग़र (चीन की सीमा) से अटलांटिक महासागर तक सल्तनत की लम्बाई पाँच हज़ार मील थी। यह इतना ज़्यादा फ़ासला है कि यदि कोई व्यक्ति पैदल सफ़र करे, जैसा कि पुराने ज़माने में किया जाता था, और प्रत्येक दिन बीस मील चले तो पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक आठ महीने से पहले नहीं पहुँच सकता।
(4)
हालाँकि वलीद का ज़माना जंगों की कामयाबी के कारण मशहूर है, लेकिन उसके अहद में विकास के काम भी ख़ूब हुए। वलीद को इमारतें बनाने का बड़ा शौक़ था। उसने मदीना की मस्जिदे नबवी को पहले से बड़ा कर दिया और उसे नए सिरे से बनाकर उसकी ख़ूबसूरती को बढ़ा दिया। मस्जिदे नबवी को नए सिरे से बनवाने की ख़ुशी में हुकूमत की ओर से मदीनावालों में नक़द रुपए बाँटे गए।
राजधानी दमिश्क़ (Damascus) में भी बड़ी शानदार मस्जिद बनाई गई जो अब तक मौजूद है। यह मस्जिद जिसे 'जामे उमवी' कहा जाता है, इतनी शानदार थी कि जब एक बार रूम का राजदूत आया तो उसने कहा—
“हम लोग समझते थे कि मुसलमानों का उत्थान कुछ दिनों के लिए है, लेकिन इस इमारत को देखकर अन्दाज़ा हुआ कि मुसलमान एक ज़िंदा रहनेवाली क़ौम हैं।"
वलीद के ज़माने में जनकल्याण के काम भी इतने अधिक हुए कि ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद अब तक इतने नहीं हुए थे। सड़कों की मरम्मत की गई और उन पर मील के चिह्न लगाए गए। तमाम रास्तों पर कुएँ बनवाए गए। मुसाफ़िरों की सहूलत के लिए जगह-जगह मेहमानख़ाने क़ायम किए गए और सारी सल्तनत में अस्पताल खोले गए। वह दमिश्क़ के बाज़ार में निजी तौर पर कामों की निगरानी करता था।
वलीद का एक बड़ा कारनामा यह है कि उसने लोगों के भीख माँगने पर पाबंदी लगा दी और अपाहिजों व मुहताजों के लिए दैनिक वज़ीफ़े तय कर दिए। अंधों और अपाहिजों की मदद के लिए आदमी मुक़र्रर किए।
वलीद ने यतीमों (अनाथों) की परवरिश और उनके शिक्षण-प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। आलिमों के वज़ीफ़े मुक़र्रर किए ताकि वे इतमीनान से लोगों को शिक्षा दे सकें। इसके अलावा वह नेक लोगों की भी माली मदद करता था।
हालाँकि वलीद एक कठोर और किसी हद तक जाबिर बादशाह था, परन्तु उसके उपरोक्त कारनामे इस बात के प्रमाण हैं कि वह एक बुद्धिमान और जागरूक बादशाह था और उसे प्रजा के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास था। निजी तौर पर उसकी ज़िंदगी धार्मिक थी। तीन दिन में एक बार क़ुरआन पूरा पढ़ लेता था। रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी सोमवार और बुधवार को रोज़े रखता था। ख़िलाफ़त के ज़माने में उसने दो हज किए। क़ुरआन हिफ़्ज़ करनेवालों को तोहफ़े देकर प्रोत्साहित करता था और रमज़ान में मस्जिदों में रोज़ेदारों के लिए खाने-पीने का इंतिज़ाम करता था।
अब्दुल मलिक और वलीद के दौर की तारीख़ में हम हज्जाज बिन यूसुफ़ को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। यह शख़्स इस्लामी ख़िलाफ़त के पूर्वी हिस्से का हाकिम था। इराक़, ईरान, तुर्किस्तान और सिंध उसके अधीन थे। उसकी हैसियत गवर्नर जनरल की थी और उसका हेड-क्वाटर कूफ़ा शहर में था। यह विचित्र स्वभाव का व्यक्ति था। एक ओर वह बड़ा ज़ालिम और अत्याचारी इनसान था तो दूसरी ओर बड़ा बुद्धिमान और शासन कार्य में निपुण था। सिन्ध और तुर्किस्तान उसी की कोशिशों से इस्लामी दुनिया का हिस्सा बने। क़ुतैबा जिसने तुर्किस्तान को फ़तह किया था और मुहम्मद बिन क़ासिम जिसने सिन्ध को फ़तह किया था, उसी के नियुक्त किए हुए सिपहसालार थे। इस ज़माने का एक बहुत बड़ा सिपहसालार मुहल्लब बिन अबी सफ़रा जिसने इराक़ और ईरान में ख़ारजियों की बग़ावत को दबाया था और जिसने पाकिस्तान पर ख़ैबर-दरे के रास्ते मुहम्मद बिन क़ासिम से भी पहले हमला किया था, उसी हज्जाज का नियुक्त किया हुआ सिपहसालार था। इसके अलावा हज्जाज का एक बड़ा कारनामा क़ुरआन को आसानी से पढ़ने के लिए उसमें एराब (मात्राएँ) एवं नुक़्ता (बिन्दुओं) का प्रयोग करना है। इससे पहले अरबी लिपि में न नुक़्ते (बिन्दु) होते थे और न ज़ेर व ज़बर (मात्राएँ)। इतिहासकार जब एक ओर हज्जाज के इन कारनामों को देखते हैं और दूसरी ओर उसके ज़ुल्म व अत्याचार को तो उनके लिए यह फ़ैसला करना कठिन हो जाता है कि हज्जाज को एक अच्छा हाकिम (प्रशासक) कहा जाए या नहीं। हज्जाज ने अब्दुल मलिक और वलीद के अहद में बाईस साल तक इस्लामी ख़िलाफ़त के पूर्वी प्रान्तों में शासन किया। इस विस्तृत इलाक़े में उमवी हुकूमत को स्थायीत्व उसी के कारण मिली। लेकिन अब्दुल मलिक और वलीद के ज़माने में जिन गवर्नरों ने सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की वे मिस्र के गवर्नर अब्दुल अज़ीज़ और अफ़्रीक़ा के गवर्नर मूसा बिन नुसैर हैं। अब्दुल अज़ीज़ इक्कीस साल तक गवर्नर रहे। ये मशहूर ख़लीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाप थे। मूसा बिन नुसैर सोलह साल तक उत्तरी अफ़्रीक़ा के गवर्नर रहे।
सुलैमान बिन अब्दुल मलिक (96 हि०/715 ई० - 99 हि०/717 ई०)
वलीद के बाद उसका भाई सुलैमान बिन अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा हुआ। हालाँकि उसने सिर्फ़ ढाई साल तक हुकूमत की पर उसके शासनकाल में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। पहली घटना वलीद के दौर के तीन मशहूर सिपहसालारों का अफ़सोसनाक अंजाम है। तुर्किस्तान के विजेता क़ुतैबा ने किसी ग़लतफ़हमी के कारण सुलैमान के ख़िलाफ़ बग़ावत करना चाही, परन्तु उसकी फ़ौज ने उसका साथ नहीं दिया और अपने ही सिपाहियों के हाथों मारा गया। मुहम्मद बिन क़ासिम को, कूफ़ा के नए गवर्नर ने जो हज्जाज बिन यूसुफ़ के इंतिक़ाल के बाद गवर्नर नियुक्त हुआ था, सिंध से वापस बुला लिया। नया गवर्नर चूँकि हज्जाज का विरोधी था, इसलिए उसने हज्जाज के तमाम रिश्तेदारों से बदला लिया। मुहम्मद बिन क़ासिम भी इस इंतिक़ाम का बेक़सूर निशाना बना और क़ैद कर दिया गया, जहाँ उसका इंतिक़ाल हो गया। मूसा बिन नुसैर से सुलैमान ने सरकारी ख़र्च के सम्बन्ध में सख़्ती से पूछ-ताछ की और जब वह संतोषप्रद जवाब न दे सका तो उससे ख़र्च वसूल कर लिए और मूसा कि ज़िंदगी का आख़िरी ज़माना बड़ी कठिनाई और तंगी में गुज़रा। इन सिपहसालारों में पहले दो के अंजाम की ज़िम्मेदारी हालाँकि सुलैमान पर नहीं है और मूसा के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि उससे जवाबतलबी न्याय एवं इनसाफ़ पर आधारित थी, परन्तु इन घटनाओं के कारण चाहे जो हों और इनकी ज़िम्मेदारी चाहे जिसपर हो, यह अपनी जगह सत्य है कि इन तीन महान सिपहसालारों का यह अफ़सोसनाक अंजाम सुलैमान के शासनकाल में हुआ और इस्लामी इतिहास के भविष्य पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा।
सुलैमान के दौर की दूसरी अहम घटना क़ुस्तनतीनिया (Constantinopel) का घेराव है। क़ुस्तनतीनिया पर यह हमला जल-थल दोनों रास्तों से किया गया था। इस हमले का नेतृत्व सुलैमान के भाई मुसलिमा बिन अब्दुल मलिक ने किया था, जो इससे पहले रूमियों के साथ जंगों में प्रसिद्धि पा चुका था। इस जंग में मुसलमानों का बहुत अधिक नुक़सान हुआ। थरैस की सख़्त बर्फ़बारी और रसद की कमी के कारण फ़ाक़े की नौबत आ गई थी, लेकिन मुसलिमा हर हाल में क़ुस्तनतीनिया फ़तह करने का प्रण किए हुए था। परन्तु इस बीच सुलैमान की मृत्यु हो गई और नए ख़लीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, जो अम्न के ख़्वाहिशमंद थे, फ़ौजों को वापस बुला लिया।
सुलैमान के दौर की तीसरी अहम घटना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का उत्तराधिकारी बनना है। सुलैमान एक दीनदार और बुद्धिमान शासक था। उसने अपने दौर में उन अत्याचारों के प्रायश्चित करने की कोशिश की थी जो वलीद के दौर में हज्जाज और दूसरे गवर्नरों के कारण लोगों को उठानी पड़ी थीं। सुलैमान को उसके सुधारवादी स्वभाव और नेक कामों के कारण तारीख़ (इतिहास) में 'मिफ़ताहुल-ख़ैर' यानी भलाई की कुंजी के नाम से जाना जाता है। उसके नेक कामों में सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण काम यह है कि उसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे आदमी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, हालाँकि शाही ख़ानदान के दूसरे अहम लोग और ख़ुद उसके अपने भाई एवं लड़के मौजूद थे। सुलैमान ने यह फ़ैसला अपने मुसाहिब (सभासद) रजाअ बिन हयात की सलाह पर किया। रजाअ ने सुलैमान से कहा था, "ख़लीफ़ा ऐसे सालेह (सदाचारी) शख़्स को बनाना चाहिए ताकि वसीयत करनेवाले को क़ब्र में अम्न (शान्ति) रहे।"
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (99 हि०/717 ई० - 101 हि०/720 ई०)
(1)
हालाँकि वलीद का दौर सांस्कृतिक विकास, जंगों की जीत और जनकल्याणकारी कामों के लिहाज़ से बेमिसाल था, लेकिन उमवी दौर में यदि कोई हुक्मराँ महान कहलाने का हक़दार है तो वह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) हैं। इन्होंने सिर्फ़ दो साल पाँच महीने ख़िलाफ़त की, लेकिन इस थोड़े समय में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की याद ताज़ा कर दी।
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा बनने से पहले बड़े ऐश और आराम की ज़िंदगी गुज़ारते थे और बड़े नाज़ुक मिज़ाज थे। आप अच्छे से अच्छा लिबास पहनते थे। एक बार जो लिबास पहन लेते फिर दोबारा नहीं पहनते थे। लेकिन ख़लीफ़ा बनने के बाद उनकी ज़िंदगी बिलकुल बदल गई। शाही ठाट-बाट से मुँह मोड़ लिया और सादा ज़िंदगी अपना ली।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु), अब्दुल मलिक और वलीद आदि हालाँकि अच्छे और क़ाबिल हुक्मराँ थे, लेकिन उनके ज़माने में लोगों पर अत्याचार भी हुए थे और सबसे बड़ी बुराई तो यह थी कि ख़िलाफ़त बादशाहत में बदल गई थी। ख़लीफ़ा अब मुसलमानों का चुना हुआ नहीं होता था, बल्कि ख़ानदान बनी उमय्या ने ताक़त के ज़ोर से सल्तनत हासिल कर ली थी और सल्तनत को अपनी जागीर बना लिया था। ख़लीफ़ा उन्हीं के ख़ानदान का आदमी हो सकता था। बैतुलमाल में जो रक़म आती थी उसे अपना माल समझते थे और उससे ज़्यादा लाभ ख़लीफ़ा के रिश्तेदार और समर्थक उठाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने इस ज़ुल्म व ज़्यादती का ख़ात्मा कर दिया। अत्याचारी और अन्यायी ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया। बैतुलमाल को प्रजा की भलाई के काम के लिए समर्पित कर दिया। उससे सिर्फ़ उन लोगों की मदद की जाती थी जो उसके हक़दार थे।
(2)
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) अपने वक़्त के बड़े आलिमों में से एक थे। उनका अख़लाक़ व किरदार भी सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) जैसा था। उनके पिता अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के भाई थे और मिस्र के प्रसिद्ध गवर्नर थे। यह बाप की तरबियत का ही नतीजा था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शुरू से ही नेक स्वभाव के थे और हुकूमत की दमनकारी नीति को पसन्द नहीं करते थे। ख़लीफ़ा चुने जाने से पहले वलीद के ज़माने के ज़ालिम गवर्नरों पर उनकी यह टिप्पणी उनके नेक स्वभाव का सबूत है—
"इराक़ में हज्जाज, शाम (सीरिया) में वलीद, मिस्र (Egypt) में क़ुर्रह बिन सुरैक, मदीना में उसमान बिन हय्यान और मक्का में ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह क़सरी – अल्लाह! तेरी दुनिया ज़ुल्म से भर गई है अब लोगों को राहत दे।"
वलीद के बाद सुलैमान और फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ख़िलाफ़त, क्या ताज्जुब इसी दुआ का नतीजा हो। वलीद के ज़माने में वह मदीना के गवर्नर थे और मस्जिदे नबवी का विस्तार उन्हीं की देख-रेख में हुआ। कहा जाता है कि वलीद के ज़माने में वलीद के हुक्म से उनसे एक ज़ालिमाना काम हो गया, जिसका उनके दिल पर इतना प्रभाव पड़ा कि ज़िंदगी का रुख़ ही बदल गया।
हालाँकि नियम के मुताबिक़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ख़लीफ़ा नियुक्त हो चुके थे, परन्तु उनकी नियुक्ति चूँकि आम मुसलमानों की सहमति से नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने ख़िलाफ़त क़बूल करने से इनकार कर दिया और ख़लीफ़ा-चुनाव के मामले को आवाम के सामने पेश करते हुए कहा—
“लोगो! मेरी इच्छा और आम मुसलमानों की सहमति के बिना ही मुझपर ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है, इसलिए मैं ख़िलाफ़त से दस्तबरदार (परित्याग) होता हूँ और तुम जिसे चाहो अपना ख़लीफ़ा बना लो।"
लेकिन आवाम ने आपकी दस्तबरदारी क़बूल नहीं की और सर्वसम्मति से आपको अपना ख़लीफ़ा चुन लिया। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) को यह यक़ीन हो गया कि किसी को आपकी ख़िलाफ़त से मतभेद नहीं है तो आपने ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी क़बूल कर ली और अवाम के सामने एक तक़रीर की जो इस लिहाज़ से अहम है कि इसमें उन बुनियादी बातों को दोहराया गया जो इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूल समझे जाते हैं और जिनपर ख़िलाफ़ते राशिदा में अमल होता रहा। आपने फ़रमाया—
“ख़ुदा ने जो चीज़ हलाल कर दी है वह क़ियामत तक हलाल है और जो चीज़ हराम कर दी है वह क़ियामत तक हराम है। मैं अपनी तरफ़ से कोई फ़ैसला करनेवाला नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के आदेशों को लागू करनेवाला हूँ। किसी को यह हक़ नहीं कि ख़ुदा कि नाफ़रमानी में उसका हुक्म माने। मैं तुममें कोई विशिष्ट आदमी नहीं हूँ, बल्कि एक मामूली इनसान हूँ। हाँ! अल्लाह ने मुझपर तुम्हारी अपेक्षा कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं।"
ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद मुलूकियत के दौर में यह पहली और आख़िरी मिसाल है कि जब ख़िलाफ़त के इस्लामी उसूलों को स्थापित करने की कोशिश की गई।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने न सिर्फ़ बैतुलमाल को नाजायज़ इस्तेमाल से बचाया, बल्कि शाही ख़ानदानवालों को भी जिन्हें बड़ी-बड़ी जागीरें और जायदादें नाजायज़ तरीक़े से मिली हुई थीं उन सबको वापस लेकर उनके असली मालिकों को लौटा दिया। इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले अपनी निजी जागीर वापस कर दी। आपने शाही ख़ानदान के लोगों के वज़ीफ़े भी उसी दर से तय किए जिस दर से आम लोगों को दिए जाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) का यह काम आसान नहीं था। कोई व्यक्ति अपनी जायदाद और माल इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। परन्तु उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपने मंसूबे पर पूरी तरह अमल करके दिखा दिया। परिणाम यह हुआ कि शाही ख़ानदान के लोग आपके विरोधी बन गए।
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की तरह ख़ुद भी बैतुलमाल से सिर्फ़ इतनी रक़म लेते थे जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी थी। इस मामले में आपने जिस एहतियात का प्रदर्शन किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) चिराग़ की रौशनी में सरकारी काम कर रहे थे कि एक शख़्स उनसे मिलने आया। काम चूँकि निजी था इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने चिराग़ बुझा दिया और अँधेरे में बातें करने लगे। उस शख़्स ने जब इसका कारण पूछा तो आपने जवाब दिया—
"यह सरकारी चिराग़ है और मैं तुमसे निजी बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चिराग़ बुझा दिया। बैतुलमाल का पैसा हम निजी काम पर ख़र्च नहीं कर सकते।"
इसी प्रकार एक बार बैतुलमाल में बहुत-से सेब आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) उन्हें आम मुसलमानों में बाँट रहे थे कि उनका छोटा लड़का एक सेब उठाकर खाने लगा। यह देखकर आपने उसके मुँह से सेब छीन लिया। वह रोने लगा और माँ से शिकायत की। माँ ने बाज़ार से सेब मँगवा दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) जब घर आए तो सेब की ख़ुशबू महसूस करके बीवी से पूछा कि सरकारी सेब तो यहाँ नहीं आया? जब बीवी ने सारी बात बताई तो आपको इतमीनान हुआ और बीवी से कहा—
"अल्लाह की क़सम! मैंने उसके मुँह से सेब नहीं छीना था, बल्कि अपने दिल से छीना था इसलिए कि मुसलमानों के हिस्से के सेब के बदले मैं अपने को अल्लाह के सामने रुसवा न कर दूँ।"
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की राजनीति की बुनियाद ज़ोर-ज़बर्दस्ती के बजाए न्याय एवं इनसाफ़ पर थी। हज्जाज बिन यूसुफ़ की शासन प्रणाली को आप इतनी नापसन्द करते थे कि आपने उसके नियुक्त किए हुए हाकिमों को तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया। आपने ज़ोर-ज़बर्दस्ती, अत्याचार और बल प्रदर्शन के बदले न्याय को सफल प्रशासन की कुंजी बताया। उमवी दौर में ज़रा ज़रा-सी बदगुमानी और संदेह पर सज़ा देना आम हो गया था। यह बात क़ानून की बरतरी (सर्वोच्चता) के उसूल के ख़िलाफ़ थी, इसी लिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में इस तरीक़े को बिलकुल बन्द कर दिया गया। आपने गवर्नरों को हुक्म दिया कि सिर्फ़ शरई सबूत पर जवाब तलब किया जाए और सज़ा दी जाए। यदि इनसाफ़ लोगों का सुधार नहीं कर सकता तो फिर किसी तरह उनका सुधार नहीं हो सकता।
एक बार ख़ुरासान के एक गवर्नर ने लिखा कि ख़ुरासानवालों को कोड़े और तलवार के सिवा कोई चीज़ दुरुस्त नहीं कर सकती। इसपर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया—
"तुम्हारा यह कहना कि ख़ुरासानवालों को कोड़े और तलवार के सिवा कोई चीज़ दुरुस्त नहीं कर सकती, बिलकुल ग़लत है। उन्हें इनसाफ़ और सच्चाई ही दुरुस्त कर सकती है और इसी को जहाँ तक संभव हो आम करो।"
न्याय के मामले में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम में फ़र्क़ नहीं करते थे। अतः आपने अपने समय में ज़िम्मियों और ग़ैर मुस्लिमों के अधिकारों की हिफ़ाज़त की। ज़िम्मी के ख़ून की क़ीमत मुसलमानों के ख़ून के बराबर क़रार दी। कोई मुसलमान ज़िम्मियों का माल नहीं हड़प सकता था। जब आपने शाही ख़ानदान से ज़मीनें लेकर उनके असल मालिकों को वापस दिलाई तो कुछ ऐसे गिरजाघरों को भी ईसाइयों को वापस दिलाया जो ग़लत तरीक़े से ले लिए गए थे। जब शहज़ादा अब्बास बिन वलीद को उसकी ज़मीन वापस करने का हुक्म दिया, जो एक ईसाई से छीनी गई थी, तो अब्बास ने अपने पक्ष में सबूत के तौर पर कहा कि यह मेरे बाप वलीद ने दी थी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने उसकी दलील को यह कहकर रद्द कर दिया कि अल्लाह की किताब वलीद के प्रमाण पर भारी है। यानी क़ुरआन के हुक्म के आगे वलीद के हुक्म की कोई अहमियत नहीं। और इस प्रकार ईसाई को ज़मीन वापस दिला दी।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के न्याय का नतीजा यह निकला कि उनके ज़माने में बहुत अधिक ग़ैर मुस्लिमों ने इस्लाम क़बूल कर लिया। सिन्ध में भी तेज़ी से इस्लाम फैला। यहाँ तक कि राजा दाहिर का लड़का जयसिंह भी इस्लाम ले आया।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में समाज-सुधार की ओर भी ध्यान दिया गया। मुसलमानों में माल व दौलत की अधिकता के कारण बहुत-सी ख़राबियाँ पैदा हो गई थीं। बहुत-से लोग शराब पीने लगे थे। स्नानगृहों में मर्द नंगे होकर नहाते थे और उनमें औरतें भी नहाने के लिए जाने लगी थीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने इन सबकी रोक-थाम की। शराब को ख़रीदना-बेचना बंद कर दिया, औरतों को हम्मामों में जाने से रोक दिया और मर्दों को तहबंद बाँधकर नहाने का आदेश दिया।
वलीद के ज़माने में जन-कल्याण के जो काम हुए थे उनका हाल हम पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने उन कामों को आगे बढ़ाया। आपके समय में ख़ुरासान और तुर्किस्तान में रास्तों पर मुसाफ़िरों के लिए सराएँ बनाई गईं जहाँ स्वस्थ मुसाफ़िर एक दिन और बीमार मुसाफ़िर दो दिन निःशुल्क रह सकता था। मुल्क में जितने अपंग और अपाहिज थे सबके नाम रजिस्टरों में लिखकर उनका ख़र्च मुक़र्रर किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने की तरह नवजात शिशु के भी वज़ीफ़े मुक़र्रर किए गए और जो ग़रीब व्यक्ति क़र्ज़ अदा नहीं कर सकता था उसके क़र्ज़ अदा करने की व्यवस्था की गई। हक़ीक़त यह है कि जनकल्याण के इन कामों को देखकर आश्चर्य होता है कि ढाई साल की अल्पावधि में इतने काम कैसे अंजाम दिए गए। यह दरअसल दमनकारी शासन प्रणाली के ख़ात्मे और ख़िलाफ़त की बहाली के कारण संभव हुआ। इन सुधारों का नतीजा यह हुआ कि पूरी इस्लामी रियासत में ख़ुशहाली आ गई और कोई सदक़ा और भीख लेनेवाला भी नहीं मिलता था।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के इन क्रान्तिकारी सुधारों ने मुलूकियत (बादशाहत अथवा राजतन्त्र) के दमनकारी शासन प्रणाली और उसके तहत पोषित स्वार्थी तबक़ा पर करारी चोट की थी। इस तबक़े की रहनुमाई शाही ख़ानदान के लोग कर रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के इन सुधारों से उन्हें यह ख़तरा हुआ कि वे ख़ानदानी बादशाहत को भी ख़त्म कर देंगे और ख़िलाफ़त को आम मुसलमानों के हवाले कर जाएँगे। अतः उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) को ज़हर देकर मार डाला। उनकी उम्र उस समय सिर्फ़ 39 साल थी।
हिशाम बिन अब्दुल मलिक (105 हि०/725 ई० - 125 हि०/743 ई०)
हालाँकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने दमनकारी शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था, परन्तु वे मुलूकियत (बादशाहत अथवा राजतन्त्र) की शासन व्यवस्था को ख़त्म करने में कामयाब न हो सके थे। सुलैमान ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के साथ यह भी फ़ैसला कर दिया था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के बाद उसका भाई यज़ीद बिन अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा होगा। सुलैमान ने यह फ़ैसला इस डर से किया था कि अगर अब्दुल मलिक की औलाद को बिलकुल नज़रअंदाज़ कर दिया जाता तो अब्दुल मलिक के घरवाले उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ख़िलाफ़त क़ायम नहीं रहने देते। अतः उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद यज़ीद द्वितीय उनकी जगह ख़लीफ़ा हुआ। यज़ीद द्वितीय ने चालीस दिन तक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के नक़्शे क़दम पर चलना चाहा और उनके द्वारा किए गए सुधारों को क़ायम रखा, लेकिन यह भारी पत्थर उससे न उठ सका और चालीस दिन बाद तमाम सुधारों को निरस्त करके वही पुरानी दमनकारी शासन व्यवस्था फिर लागू कर दी। चार साल चार महीने हुकूमत करने के बाद यज़ीद का इंतिक़ाल हो गया और उसका भाई हिशाम बिन अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा हो गया।
हिशाम, जिसने बीस साल हुकूमत की, ख़ानदान बनी उमैय्या का आख़िरी बड़ा शासक है। वह बड़ा नेक, मितव्ययी, चतुर और कुशल प्रशासक था। इतिहासकारों ने लिखा है कि उसमें अमीर मुआविया का ज्ञान एवं चिन्तन और अब्दुल मलिक का उत्साह एक साथ जमा हो गया था। उसके इनसाफ़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बैतुलमाल में उस वक़्त तक आमदनी की रक़म दाख़िल नहीं करता था जब तक चालीस आदमी यह गवाही न दे देते कि यह रक़म जाइज़ तरीक़े से हासिल की गई है। वह इनसाफ़ में मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम के बीच फ़र्क़ नहीं करता था। उसके अहद में शाम (सीरिया) में रुसाफ़ा और सिंध में मंसूरा के और महफ़ूज़ के शहर आबाद हुए।
हिशाम के ज़माने में ख़ुरासान, तुर्किस्तान, अरमीनिया, आज़रबाइजान और उत्तरी अफ़्रीक़ा में सख़्त बग़ावतें और लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन उन सब बग़ावतों को दबा दिया गया। ख़ुरासान और तुर्किस्तान की लड़ाइयों में वहाँ के हाकिम नसर बिन सैयार ने जो एक कुशल प्रशासक था, बहुत नाम कमाया। अरमीनिया और आज़रबाइजान पर ग़ैर मुस्लिम तुर्कों की एक शाखा ख़ज़र ने, जो दक्षिण रूस पर हुक्मराँ थी, लगातार हमले किए परन्तु उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया और उमवी शहज़ादा मरवान बिन अब्दुल मलिक दाग़िस्तान से गुज़रता हुआ ख़ज़र की राजधानी बलंजर तक पहुँच गया। इन हमलों के कारण ख़ज़र सल्तनत की राजधानी कई सौ मील उत्तर में वालगा नदी के किनारे आतिल नामक स्थान पर ले जाई गई।
एशिया-ए-कोचक में रूमियों के साथ सख़्त लड़ाइयाँ हुईं। इन लड़ाइयों में वलीद और सुलैमान के दौर की तरह इस बार भी उमवी शहज़ादा मुसलिमा बिन अब्दुल मलिक ने बड़े कारनामे अंजाम दिए।
उत्तरी अफ़्रीक़ा में बर्बर नव मुस्लिमों ने हुकूमत की ग़लत नीतियों के कारण कई बार सख़्त बग़ावतें कीं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन्हें दबा दिया और ख़िलाफ़ते दमिश्क़ का लश्कर पहली बार मराकश के दक्षिण में रेगिस्तान को पार करके उस इलाक़े में दाख़िल हो गया जो आजकल 'सीनीगाल' और 'माली' कहलाता है और उस ज़माने में सूडान कहलाता था। यहाँ से सूसुल और बहुत-सा माले ग़नीमत हासिल हुआ। मराकश का सुदूर दक्षिणी भाग सोस अक़्सा भी उसी ज़माने में इस्लामी रियासत का हिस्सा बना और वहाँ के वासियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया।
हिशाम के ज़माने में सिन्ध में इस्लामी शक्ति और मज़बूत हुई। सिन्ध का गवर्नर जुनैद (107 से 111 हि०) बड़ा योग्य सूबेदार था। उसने कश्मीर तक लगभग तमाम इलाक़े जीत लिए जो अब पाकिस्तान कहलाता है। इसके अलावा उसने भारत में मारवाड़, उज्जैन, गुजरात और भड़ोच तक सारा इलाक़ा फ़तह कर लिया। हालांकि बाद के सूबेदार इन इलाक़ों पर क़बज़ा बरक़रार नहीं रख सके।
हिशाम के अहद की फ़ौजी मुहिमों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंदलुस के गवर्नर अब्दुर्रहमान नमाफ़क़ी का फ़्रांस पर हमला है। अब्दुर्रहमान प्रेनीज़ को पार करके फ़्रांस में दाख़िल हुआ और दक्षिणी एवं पश्चिमी फ़्रांस को फ़तह करता हुआ लूइ नदी के किनारे तोरस तक पहुँच गया जो पेरिस से सिर्फ़ डेढ़ सौ मील दूर है। यहाँ मुसलमानों का यूरोप की संयुक्त सेना से मुक़ाबला हुआ। दो दिन सख़्त लड़ाई हुई, लेकिन दूसरे दिन अब्दुर्रहमान शहीद हो गया। उसकी शहादत से मुसलमानों में मतभेद हो गया जिसके कारण मुसलमान फ़ौजें रात के अंधेरे में वापस हो गईं। दूसरे दिन मैदान ख़ाली देखकर ईसाई बहुत हैरान हुए परन्तु उन्हें मुसलमानों का पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई।
बनी उमय्या का पतन
हिशाम का जानशीन (उत्तराधिकारी) वलीद बिन यज़ीद बिन अब्दुल मलिक, जो वलीद द्वितीय कहलाता है, एक अयोग्य और ऐयाश हुक्मराँ था। उसकी ज़िंदगी में अजीब विरोधाभास था। शराब व कबाब में भी मस्त रहता था और नमाज़ भी पाबन्दी से पढ़ता था। उसकी अयोग्यता के कारण अरबों में क़बाइली भेद-भाव ने ज़ोर पकड़ लिया और अन्ततः वह कुछ महीने हुकूमत करने के बाद उसी जातीय संकीर्णता का शिकार होकर मारा गया। जब लोग उसे क़त्ल करने के लिए महल में दाख़िल हुए तो वलीद क़ुरआन खोलकर पढ़ने लगा और कहा कि “मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) क़ुरआन तिलावत करते हुए शहीद हुए थे उसी प्रकार मेरा भी अन्त हो।"
वलीद द्वितीय का जानशीन यज़ीद बिन वलीद या यज़ीद तृतीय धर्मपरायण, इबातगुज़ार इंसान था। उसको 'यज़ीद नाक़िस' भी कहते हैं। उसने ख़िलाफ़त को इस्लामी रूप देने का संकल्प किया था। परन्तु उसकी ख़िलाफ़त अभी ठीक प्रकार से जमी भी नहीं थी कि उसके मुक़ाबले में दावेदार खड़े हो गए। छः माह बाद उसका इंतिक़ाल हो गया। यज़ीद तृतीय का जानशीन उसका भाई इबराहीम बिन वलीद हुआ परन्तु अब शाही ख़ानदान के लोगों के बीच गृह युद्ध शुरू हो चुका था और एक दूसरे शहज़ादे मरवान बिन मुहम्मद ने, जो अब्दुल मलिक का भतीजा था, तीन-चार माह बाद ही उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी और ख़ुद हुक्मराँ बन बैठा।
मरवान द्वितीय एक क़ाबिल, अनुभवी और साहसी व्यक्ति था। वह 'मरवानुलहिमार' के नाम से भी मशहूर था। ख़ज़र तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में उसने अपनी फ़ौजी क़ाबिलियत का अच्छा सबूत दिया था। परन्तु सल्तनत के अन्दरूनी हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वह उनपर क़ाबू नहीं पा सका। हुक्मराँ ख़ानदान में भी मतभेद पैदा हो गए थे। अरब भी दो गिरोहों- यमनी और मिस्री क़बीले में बँट गए थे और एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे थे। सल्तनत में हर जगह विद्रोह और बग़ावतें हो रही थीं। इनमें से ख़तरनाक बग़ावत बनी हाशिम की थी। बनी हाशिम चूँकि उस ख़ानदान से थे जिसमें रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हुए हैं, इसलिए वे स्वयं को ख़िलाफ़त का बनी उमय्या से ज़्यादा अधिकारी समझते थे।
बनी हाशिम में भी दो गिरोह पैदा हो गए थे। एक वे जो हज़रत अली को और उनके बाद उनकी औलाद को ख़िलाफ़त का हक़दार समझते थे। बाद में इसी गिरोह में से कुछ लोगों ने शिया फ़िरक़ा (सम्प्रदाय) का रूप ले लिया और वे 'असना-अशरी' कहलाए। [असना-अशरी इसलिए कहा जाता है कि शियों का अक़ीदा बारह इमामों पर है जो हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में हुए। बारह को अरबी में असना अशर कहते हैं। इसलिए शीया ख़ुद को असना अशरी कहते हैं।
बारह इमाम निम्नलिखित हैं:
1. हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) (600 ई० से 661 ई०)
2. हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) (3 हि०/624 ई० से 50 हि०/670 ई०)
3. हज़रत हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) (4 हि०/626 ई० से 61 हि०/680 ई०)
4. इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन (रज़ियल्लाहु अन्हु) (38 हि०/659 ई० से 95 हि०/713 ई०)
5. इमाम मुहम्मद बाक़र (57 हि०/677 ई० से 114 हि०/732 ई०)
6. इमाम जाफ़र सादिक़ (80 हि०/699 ई० से 148 हि०/765 ई०)
इमाम जाफ़र सादिक़ बनी उमय्या के आख़िरी और बनी अब्बास के शुरू के दौर में थे। वे अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे। शीया क़ानून या फ़िक़्ह उन्हीं के नाम पर 'फ़िक़्ह जाफ़री' कहलाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ तक शीयों में और अन्य मुसलमानों में कोई मज़हबी मतभेद नहीं था, लेकिन उनके बाद शीयों ने बतदरीज एक अलग और स्थाई फ़िरक़े की शक्ल इख़तियार कर ली।
7. इमाम मूसा काज़िम (128 हि०/745 ई० से 183 हि०/799 ई०)
8. इमाम अली रज़ा (148 हि०/765 ई० से 203 हि०/818 ई०)
9. इमाम मुहम्मद जव्वाद रज़ी (195 हि०/811 ई० से 220 हि०/835 ई०)
10. इमाम अली नक़ी हादी (212 हि०/828 ई० से 254 हि०/868 ई०)
11. इमाम हसन अस्करी (232 हि०/847 ई० से 260 हि०/873 ई०)
12. इमाम मेहदी (255 हि०/869 ई०)
ईमाम मेहदी हसन अस्करी के बेटे थे। चार साल की उम्र में सामिरा की एक गुफा में ग़ायब हो गए। शीया उनको ज़िन्दा मानकर इमामे मुन्तज़र, इमामे ज़मा, मेहदी-ए-दौरान के नामों से याद करते हैं और समझते हैं कि क़ियामत से पहले उनका ज़ुहूर होगा।]
दूसरा गिरोह रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चाचा हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद को ख़िलाफ़त दिलाना चाहता था। शुरू में दोनों गिरोहों ने मिलकर बनी उमय्या की हुकूमत के ख़िलाफ़ बग़ावतें कीं लेकिन बाद में अब्बासी गिरोह ग़ालिब हो गया।
बनी अब्बास का आन्दोलन उमर बिन उब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के ज़माने से ही शुरू हो गया था, हिशाम के दौर में यह काफ़ी व्यापक हो गया। ख़िलाफ़त के असल दावेदार अहले बैअत थे, यानी हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की वह औलाद जो हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से थी या फिर हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की वह औलाद जो फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से नहीं थी और जो ‘अलवी' कहलाती थी। इमाम हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की शहादत के बाद शीयाने अली ने इमामत के पद पर इमाम हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया था, परन्तु उन्होंने इमामत क़बूल नहीं किया। तब शियों ने हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ग़ैर फ़ातिमी बेटे मुहम्मद बिन हनफ़िया (21 हि० से 81 हि०) को इमाम बना लिया और इस प्रकार इमामत का पद अहले बैअत से अलवी शाखा में हस्तांतरित हो गया। मुहम्मद बिन हनफ़िया के बाद उनके बेटे अबू हाशिम अब्दुल्लाह जानशीन हुए और ईरान में उनकी दावत गुप्त रूप से फैलती रही। 100 हिजरी में अबू हाशिम अब्दुल्लाह का इंतिक़ाल शाम (सीरिया) में हो गया। उस समय उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पोते मुहम्मद बिन अली क़रीब मौजूद थे इसलिए अबू हाशिम ने उन्हें जानशीन मुक़र्रर करके इमामत का पद उनके सुपुर्द कर दिया और इस प्रकार इमामत अलवियों से अब्बासियों में हसतांतरित हो गई। बनी हाशिम की यह दावत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से हिशाम तक गुप्त रही और इराक़ और ख़ुरासान के बड़े हिस्से में फैल गई। 126 हिजरी में मुहम्मद बिन अली का इंतिक़ाल हो गया और उनके बाद उनके लड़के इबराहीम उनके जानशीन हुए। उनका मरकज़ शाम (सीरिया) में हमीमा नामक स्थान में था। उनके दौर में इस तहरीक ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया और मशहूर ईरानी अबू मुस्लिम ख़ुरासानी उसी ज़माने में अब्बासी तहरीक के समर्थक की हैसियत से दाख़िल हुआ। उसने एक ओर अरबों को आपस में लड़ाया और दूसरी तरफ़ ईरानियों को अरबों के ख़िलाफ़ उभारा। इस जगह यह बात ग़ौर करने की है कि मुहम्मद बिन अली ने अबू मुस्लिम को हिदायत की थी कि ख़ुरासान में कोई अरबी बोलनेवाला ज़िन्दा न छोड़ा जाए। मरवान के दौर में इस साज़िश का भंडाफोड़ हो गया और इबराहीम को क़त्ल कर दिया गया। अब इबराहीम का भाई अबुल अब्बास अब्दुल्लाह बिन अली जानशीन हुआ। उसने भी हुक्म दिया कि ख़ुरासान में कोई अरब ज़िन्दा न छोड़ा जाए। उसने इबराहीम के ग़म में काला लिबास और काला झण्डा अब्बासियों का चिह्न क़रार दिया।
हम पढ़ चुके हैं कि ईरानी शुरू ही से अरबों से नफ़रत करते थे और अरब ईरानियों से। जब ईरान पर अरबों का क़बज़ा हुआ तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने न्याय पर आधारित हुकूमत क़ायम करके इस नफ़रत को कम करने की कोशिश की, लेकिन बनी उमय्या के हुक्मरानों ने उन उसूलों पर चलना छोड़ दिया। ईरानियों को भी हुकूमत से शिकायत बढ़ती चली गई। वह अब मुसलमान हो गए थे और मुसलमान होने की हैसियत से अरबों के बराबर अधिकार चाहते थे। जब उनके साथ बराबर का सुलूक नहीं किया गया तो वे बनी उमय्या का तख़्ता पलटने की चिन्ता करने लगे और अपना मक़सद हासिल करने के लिए उन्होंने बनी हाशिम का साथ दिया।
बनी उमय्या के ज़माने में अरबों और ईरानियों के बीच नफ़रत के अलावा ख़ुद अरबों के अन्दर क़बाइली संकीर्णता और मतभेद भी काफ़ी बढ़ गए थे। यह मुसलमानों की बड़ी बदक़िस्मती है कि रंग और नस्ल के ये मतभेद जिनको मिटाने के लिए इस्लाम आया था, इतनी जल्दी फिर सिर उठाने लगे और एक क़बीला दूसरे क़बीलेवालों के साथ ज़ुल्म व ज़्यादती करने लगा। इस मतभेद के कारण अरबों की शक्ति कमज़ोर हो गई और बनी उमय्या का सबसे बड़ा सहारा चूँकि सिर्फ़ अरब थे, इसलिए उनके कमज़ोर पड़ने से बनी उमय्या की सल्तनत कमज़ोर पड़ गई।
इस्लामी दुनिया की यह हालत थी कि बनी हाशिम के समर्थकों ने ईरानियों की मदद से ख़ुरासान में ज़बरदस्त बग़ावत कर दी। हिशाम के अयोग्य जानशीन इस बग़ावत का मुक़ाबला न कर सके। इस संघर्ष में एक ईरानी सरदार अबू मुस्लिम ख़ुरासानी से बनी हाशिम को बड़ी मदद मिली। वह बड़ा अत्याचारी और ज़ालिम ईरानी था, परन्तु उसके अन्दर एक ख़ूबी यह थी कि वह एक अच्छा संचालक एवं व्यवस्थापक था। बनी हाशिम के ये समर्थक मावरा-उन-नहर और ईरान पर क़बजा करने के बाद इराक़ में दाख़िल हो गए जहाँ बनी उमय्या के आख़िरी हुक्मरान मरवान बिन मुहम्मद ने ज़ाब नदी के किनारे मुक़ाबला किया लेकिन इस बुरी तरह उसकी हार हुई कि मैदान छोड़कर उसे भागना पड़ा। बाद में वह पकड़ा गया और उसे क़त्ल कर दिया गया। राजधानी दमिश्क़ पर बनी हाशिम का क़बज़ा हो गया और बनी उमय्या की हुकूमत ख़त्म होकर बनी हाशिम की शाखा बनी अब्बास की हुकूमत क़ायम हो गई।
अध्याय-9
ख़िलाफ़त, मुलूकियत (राजतन्त्र) की ओर!
ख़ानदान बनी उमय्या की हुकूमत 92 साल तक चली। 14 साल अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) का ख़ानदान और 78 साल मरवान का ख़ानदान हुक्मराँ रहा। यह मुलूकियत (बादशाहत, राजतन्त्र) की स्थापना और स्थायित्व का ज़माना है। अमीर मुआविया के ज़माने में अत्याचार और मुलूकियत (राजतन्त्र) के बुरे नतीजे अधिक स्पष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वे बल प्रयोग के साथ-साथ नर्मी, बुद्धि और समझौते से भी काम लेने की कोशिश करते थे। लेकिन अब्दुल मलिक के बाद राजतन्त्र अपनी तमाम ख़राबियों के साथ सामने आ गया। हालाँकि हुक्मराँ अब भी 'ख़लीफ़ा' और 'अमीरुल मोमिनीन' कहलाते थे और उन्होंने अपने लिए 'शाह' या सुल्तान की उपाधि अभी तक नहीं अपनाई थी। ख़लीफ़ा की नियुक्ति के समय बैअत अब भी ली जाती थी, परन्तु उसकी हैसियत अब सिर्फ़ दिखावा थी। बैअत की रस्म से अगर कोई बात ज़ाहिर होती थी तो वह सिर्फ़ यह कि ख़िलाफ़त और मुसलमानों की आम सहमति एक-दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। परन्तु राय देने की आज़ादी अब ख़त्म हो चुकी थी। ताक़त अपने नग्न रूप में सामने आ चुकी थी और विरोध करना जान से हाथ धोने के बराबर था। इस बात ने मुलूकियत को मज़बूती दी।
राजतन्त्र के कारण इस्लामी दुनिया उन गुणों से वंचित हो गई जो ख़िलाफ़ते राशिदा की विशेषता समझे जाते थे और इस्लामी दुनिया के राजनीतिक ढाँचे में निम्न ख़राबियाँ आने लगीं :
1. हुक्मराँ एक आम इनसान नहीं रहा, जैसा कि ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में था। अब दमिश्क़ के हुक्मरानों ने ईरान और रूम के बादशाहों की तरह शाहाना ज़िन्दगी अपना ली। उन्होंने रहने के लिए शानदार महल बनवाए जिनपर बहुत अधिक धन ख़र्च किए गए। सुरक्षा के लिए दरबान और अंगरक्षक नियुक्त किए। अब लोग हुक्मराँ से सीधे नहीं मिल सकते थे। शाही महल के कर्मचारी और दरबान उनके और आवाम के बीच माध्यम बन गए और इस तरह हुक्मराँ और अवाम के बीच वह सीधा सम्बन्ध ख़त्म हो गया जो ख़िलाफ़ते राशिदा की विशेषता समझी जाती थी। इस माहौल में हुक्मराँ ख़ुद को आम इनसान से उच्च समझने लगे।
2. बैतुलमाल अब प्रजा की अमानत नहीं रहा, बल्कि बादशाह का निजी ख़ज़ाना बन गया। बादशाह अपनी मरज़ी से जिस तरह चाहे बैतुलमाल की रक़म लुटा सकता था। बादशाह से हिसाब पूछने का हक़ किसी को नहीं रहा। अब नाजायज़ तरीक़े से टैक्स (Tax) वुसूल करके भी बैतुलमाल में जमा किया जाने लगा।
3. ख़िलाफ़ते राशिदा में लोगों को हुक्मरानों से किसी भी मामले में सवाल पूछने की आज़ादी थी, बल्कि इस मामले में ख़लीफ़ा लोगों को प्रोत्साहित करते थे, परन्तु अब अभिव्यक्ति की यह स्वतन्त्रता ख़त्म हो गई और सच एवं हक़ बात बोलने पर क़त्ल की सज़ा दी जाने लगी।
4. ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में अदालत के फ़ैसलों में बड़े से बड़ा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, बल्कि क़ाज़ी (जज) ख़लीफ़ा तक को अदालत में तलब कर लेता था और ख़लीफ़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे सकता था, लेकिन मुलूकियत के ज़माने में बादशाह तो बड़ी चीज़ है, क़ाज़ी को शाही ख़ानदान के लोगों, गर्वनरों और उनसे सम्बन्धित बाअसर लोगों के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले देना लगभग असंभव हो गया।
5. ख़िलाफ़ते राशिदा की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सलाहकार समिति को बुनियादी महत्त्व दिया जाता था, मुलूकियत (राजतन्त्र) के दौर में इसे भी ख़त्म कर दिया गया। यदि ख़लीफ़ा कभी सलाह-मशविरा लेता था तो सिर्फ़ अपने समर्थकों और अपने ख़ानदान और क़बीलेवालों से और वह भी अपने तय किए हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। प्रजा और मुसलमानों की भलाई इस मशविरे का असल मक़सद नहीं होता था। सलाहकार समिति के इस प्रकार ख़ात्मे से एक नुक़सान यह हुआ कि इस्लामी दुनिया में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के विकास का रास्ता रुक गया।
6. ख़िलाफ़ते राशिदा में क़ानून को बरतरी (सर्वोच्चता) हासिल थी। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (प्रथम चार ख़लीफ़ा) न ख़ुद कभी (किसी भी हालत में) शरीअ़त की सीमा से बाहर क़दम रखते थे और न किसी को इसकी इजाज़त देते थे। बनी उमय्या के दौर में हालाँकि इस्लामी शरीअ़त को क़ानून की हैसियत हासिल रही और उसकी बरतरी से इनकार नहीं किया गया, लेकिन हुक्मराँ और उनके निकट के लोग जहाँ भी मौक़ा मिलता और जहाँ भी उनका स्वार्थ होता, शरीअ़त की सीमा का उल्लंघन करने से नहीं चूकते थे। राजनीतिक एवं निजी जीवन में शरीअ़त की सीमा का यह उल्लंघन बहुत स्पष्ट था। इस प्रकार दीन (धर्म) और राजनीति एक-दूसरे से दूर होते गए और यह समझा जाने लगा कि राजनीतिक मामले का फ़ैसला करना बादशाहों का काम है, न कि आलिमों का।
7. चूँकि हुक्मरानों का सम्बन्ध एक विशेष क़बीले और एक विशेष नस्ली अरबवासियों से था, इसलिए वे 'अमीरुल मोमिनीन' से ज़्यादा 'अमीरुल अरब' बन गए थे। वे सबसे पहले अपने क़बीले और उसके बाद अपनी नस्ल के लोगों के हित का ख़याल रखते थे, क्योंकि उनकी शक्ति बनी उम्मया और अरबों पर निर्भर थी। इस चीज़ ने अरब और अजमी (ग़ैर अरब) के उस विभाजन को पुनः ज़िन्दा कर दिया जिसकी जड़ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ुतबा-ए-हिज्जतुल विदअ में काट दी थी और ख़िलाफ़ते राशिदा के समय में जो सिर नहीं उठा सका था। बनी उमय्या के हुक्मरानों के इस व्यवहार के कारण ईरानी मुसलमानों में ईरानी जातीवाद की प्राचीन भावना ख़त्म नहीं हो सकी। ईरानी जातीवाद का यह आन्दोलन इतिहास में 'शऊबियत' के नाम से जाना जाता है।
मुलूकियत (राजतन्त्र) का स्थायित्व
यहाँ कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह सवाल पैदा होता है कि इस्लामी ख़िलाफ़त इतनी जल्दी यानी सिर्फ़ तीस साल की अवधि में मुलूकियत (राजतन्त्र) में कैसे बदल गई? इसके दो कारण हैं—
प्रथम यह कि प्रजातन्त्र या किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की कामयाबी प्रजा के विवेक के अलावा वक़्त के हालात पर भी है। उदाहरणत: यह कि समाज का विकास किस प्रक्रिया में है और उसमें एकता का एहसास कहाँ तक है? प्राचीन काल में छोटी बस्तियों और इलाक़ों में एकता आसानी से पैदा हो सकती थी और यही कारण है कि प्रजातन्त्र अपने प्रारम्भिक काल में शहरों और बस्तियों में अस्तित्व में आया, परन्तु एक विशाल सल्तनत में जिसका एक इलाक़ा दूसरे इलाक़ों से प्राकृतिक अवरोधों के कारण कटा हुआ हो, जहाँ दो स्थानों के बीच के फ़ासले दिनों और महीनों में तय होते हों और उस सल्तनत की प्रजा विभिन्न रंग, नस्ल और भाषाओं से सम्बन्ध रखती हो और वे भी उन ही हथियारों से लैस हों जो फ़ौज के पास होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रजातान्त्रिक एवं प्रतिनिधि सरकार नहीं बन सकती। ऐसे माहौल में हर वह व्यक्ति, जो कुछ लोगों को अपने गिर्द जमा करने की योग्यता रखता हो, बग़ावत कर सकता है और प्रजातान्त्रिक एवं प्रतिनिधि सरकार को ख़त्म कर सकता है। प्राचीन काल में यूनान और रूम में प्रजातान्त्रिक प्रणाली को बढ़ावा देने की सबसे ज़्यादा कोशिश की गई थी। परन्तु यूनान में प्रजातन्त्र उसी समय तक चला जब तक 'नगर-सरकारें' अस्तित्व में रहीं, परन्तु जब फ़ीलक़ोस और सिकन्दर ने उन नगर-सरकारों को ख़त्म कर दिया तो प्रजातन्त्र भी ख़त्म हो गया। रूम को भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब तक सत्ता रूम शहर के नागरिकों के हाथ में रही, प्रजातन्त्र क़ायम रहा, लेकिन जैसे-जैसे हुकूमत बढ़ती गई उसमें डिक्टेटरशिप का रुझान पैदा होता गया और जब जूलियस सीज़र ने रूम को एक विशाल सल्तनत की शक्ल दे दी तो वह ख़ुद बादशाह बन गया और प्रजातन्त्र ख़त्म हो गया।
यही कारण है कि दुनिया में जब तक प्रजातन्त्र के विकास के लिए भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक माहौल नहीं बना, प्रजातन्त्र क़ायम नहीं हो सका। यह माहौल उन्नीसवीं शताब्दी में उस समय पैदा हुआ जब यूरोप में छोटी-छोटी क़ौमें अस्तित्व में आ गईं और इस प्रकार उनमें जातीय एवं भाषाई एकता पैदा हो गई। अब हर क़ौम के अन्दर आन्तरिक मतभेद कम से कम हो चुके थे। संचार माध्यम (सड़क, तार, अख़बार) बहुत तरक़्क़ी कर चुका था और फ़ौजें ऐसे हथियारों से लैस हो गई थीं जो अवाम के पास नहीं थे और जिनके द्वारा वह बग़ावत करनेवालों को आसानी से दबा सकती थीं। जब यह माहौल पैदा हो गया तो यूरोप में जनता की प्रतिनिधि सरकारें क़ायम हो गईं।
मुसलमानों को भी शुरू में ऐसे ही हालात का मुक़ाबला करना पड़ा। ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में इस्लामी सल्तनत अपनी विशालता में रूम की उस हुकूमत से बड़ी थी जिसे ख़त्म करके जूलियस सीज़र ने बादशाहत क़ायम की थी। फिर यह ख़िलाफ़त रूमी प्रजातन्त्र की तरह तीन सौ साल के विकास का नतीजा नहीं थी, बल्कि तीस साल की अल्प अवधि में अस्तित्व में आई थी। ख़िलाफ़त की सीमाओं में जो क़ौमें आबाद थीं वे रंग, नस्ल, भाषा और धर्म के लिहाज़ से एक-दूसरे से भिन्न थीं। ख़ुद अरब जो इस्लामी ख़िलाफ़त के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, अपनी भाषाई, नस्ली और मज़हबी एकता के बावजूद क़बाइली संकीर्णता के जज़्बे से अभी तक ख़ुद को पूरी तरह आज़ाद नहीं कर सके थे। ऐसी सूरत में ख़िलाफ़त या प्रजातान्त्रिक ढाँचे को कोई चीज़ क़ायम रख सकती थी तो वह मुसलमानों का सामूहिक विवेक था।
ख़िलाफ़ते राशिदा में मुसलमानों के सामूहिक विवेक ने इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में ख़िलाफ़त का रास्ता इख़तियार किया, लेकिन सल्तनत के सामूहिक हालात चूँकि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं थे इसलिए अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की बग़ावत कामयाब हो गई और राजतन्त्र की बुनियाद पड़ी। इस प्रकार मुसलमानों की सामूहिक भावना को ठेस पहुँची और उसे क़ायम करने का मौक़ा न मिल सका। परन्तु यदि उसे क़ायम करने का मौक़ा मिल भी जाता तो भी उस वक़्त के हालात के तहत प्रजातन्त्र देर तक क़ायम नहीं रह पाता।
आलिमों (विद्वानों) की भूमिका
इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक काल को इस्लामी विशेषताओं के लिहाज़ से तीन कालों में बाँटा गया है। यानी सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का काल, ताबिईन का काल और तबा ताबिईन का काल। यह विभाजन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की एक मशहूर हदीस के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ है—
“अच्छा दौर मेरा है, फिर वह दौर जो उसके बाद आएगा, और फिर वह जो उसके बाद आएगा।"
आलिमों ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए बताया है कि पहले दौर से मुराद अहदे सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) है यानी उन लोगों का दौर जिनकी तरबियत ख़ुद रसूले पाक (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने की। दूसरे दौर से मुराद उन लोगों का दौर है जिन्होंने सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से तरबियत हासिल की और तीसरे दौर से मुराद उन लोगों का दौर है, जिन्होंने ताबिईन (दूसरे दौर के लोगों) की संगति पाई। इस व्याख्या के अनुसार बनी उमय्या की हुकूमत का ज़माना दूसरे दौर से सम्बन्धित है। हालाँकि इस दौर के प्रारंभ और अन्त का सम्बन्ध पहले और तीसरे दौर से भी है।
भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इस्लाम के बुनियादी आदेशों में से हैं और इस फ़र्ज़ को इस दौर में जिस तबक़े के लोगों ने पूरा किया, वह आलिमों और ताबिईन का तबक़ा है। इस फ़र्ज़ को अदा करते हुए इस दौर के आलिमों ने दरअस्ल क़ुरआन के उस आदेश का पालन किया जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के बीच एक जमाअत ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से रोके।
ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने में शिक्षा की जो व्यापक व्यवस्था की गई थी उसके नतीजे में और सहाबा किराम की निजी जिद्दोजुहद के कारण इस्लामी दुनिया में क़ुरआन एवं सुन्नत का ज्ञान रखनेवाले आलिम हज़ारों की तादाद में तैयार हो चुके थे। यह वह जमाअत थी जिसने क़ुरआन व सुन्नत एवं इस्लामी दृष्टिकोण की व्याख्या बिना किसी ख़ौफ़, लालच और निजी स्वार्थ के की। यह वह गिरोह था जिसने बादशाहत को इस्लामी राजनीति की बुनियाद के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया और जब यह तलवार के ज़ोर पर थोप दिया गया तो इसे सिर्फ़ इसलिए क़बूल कर लिया कि मुसलमान आपसी ख़ून-ख़राबे से बच जाएँ। मुलूकियत के कारण पैदा होनेवाली बहुत-सी ख़राबियों और नुक़सानों की क्षतिपूर्ति इन आलिमों ने कर दी। उन्होंने हुक्मरानों की ग़लत बातों को इस्लाम का हिस्सा नहीं बनने दिया और अत्याचार एवं दमन के मुक़ाबले में आम लोगों का पक्ष लिया। उन्हें जब भी मौक़ा मिलता वह हक़ बात कहने में झिझक महसूस नहीं करते थे।
आलिमों का यह तबक़ा हालाँकि हुक्मरानों के रवैये को पसन्द नहीं करता था और वे सरकारी पदों को क़बूल नहीं करते थे, लेकिन चूँकि सल्तनत के बुद्धिजीवी और जागरूक लोग आलिम ही थे, इसीलिए हुकूमत उनका सहयोग लेने पर मजबूर थी। अत: न्याय और शिक्षा के विभाग आलिमों के ही हाथ में थे। इस दौर के क़ाज़ियों (जजों) ने दमनकारी शासन व्यवस्था के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था अदालत को आज़ाद रखने की कोशिश की और उनके निष्पक्ष फ़ैसले अवाम को इनसाफ़ देते रहे। उस ज़माने के क़ाज़ियों में सबसे मशहूर क़ाज़ी शुरेह हुए, जो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से अब्दुल मलिक की ख़िलाफ़त की शुरूआत तक साठ साल कूफ़ा के क़ाज़ी रहे। उन्होंने न्यायपालिका में कई सुधार किए। ख़ुफ़िया तहक़ीक़ात का तरीक़ा राइज किया, अदालत के नए-नए नियम बनाए। उनके फ़ैसले सुनने के लिए बड़े-बड़े आलिम अदालत में आते थे।
आलिमों ने हुक्मरानों के ग़लत फ़ैसलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया और हक़ की आवाज़ बुलन्द रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अतः जब अब्दुल मलिक ने अपनी ज़िंदगी में अपने दो बेटों को एक के बाद दूसरे को जानशीन (उत्तराधिकारी) बनाना चाहा तो मशहूर ताबई सईद बिन मुसय्यिब ने विरोध किया, जिसके लिए उन्हें क़ैद और कोड़े से मारे जाने की सज़ा मिली। हज्जाज ने जब बसरा और कूफ़ा के नव मुस्लिमों पर जिज़्या लगाया तो आलिमों ने कड़ा विरोध किया और जब अब्दुर्रहमान बिन अशअस ने हज्जाज के ज़ुल्मों के विरुद्ध बग़ावत की तो आलिमों की बड़ी तादाद जिनमें सईद बिन ज़ुबैर, इबराहीम नख़ई और शअबी जैसे बुज़ुर्ग शामिल थे, अब्दुर्रहमान का साथ दिया और हक़ का झण्डा उठाने के ही कारण सईद बिन ज़ुबैर को शहीद होना पड़ा। इस बग़ावत के सिलसिले में ग़ौर करनेवाली बात यह है कि इमाम शअबी (रहमतुल्लाह अलैह) जैसे उन आलिमों ने भी जो हुकूमत को सहयोग देते थे, बाग़ियों का साथ दिया था। इस प्रकार जब हिशाम के ज़माने में हज़रत ज़ैद बिन अली ने दमनकारी शासन का तख़्ता पलटना चाहा तो इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) ने उनका पक्ष लिया।
बनी उमय्या की हुकूमत के सम्बन्ध में विद्वानों के आचरण का उस काल के दो सुप्रसिद्ध विद्वानों के कथन से हम भली-भाँति अनुमान लगा सकते हैं। मदीना के विद्वान सईद बिन मुसय्यिब (रहमतुल्लाह अलैह) कहा करते थे—
"बनी मरवान इनसानों को भूखा रखते हैं और कुत्तों का पेट भरते हैं।"
और बसरा के प्रसिद्ध विद्वान इमाम हसन बसरी (रहमतुल्लाह अलैह) कहा करते थे—
"इस ज़माने के अमीरों (उच्चाधिकारियों) की तलवारें हमारी ज़बानों से आगे बढ़ गई हैं। जब हम बात करते हैं तो वे हमें तलवार से जवाब देते हैं।" [तारीख़े इस्लाम (उर्दू) द्वितीय भाग, लेखक शाह मुईनुद्दीन, प्रकाशन दारुल मुसन्निफ़ीन, आज़मगढ़, पृष्ठ 363]
उस काल के हुक्मराँ यद्यपि जनता का दिल नहीं जीत सके, परन्तु आलिमों ने अपनी सच्ची बातों से जनता को अपना प्रशंसक बना लिया था। अवाम के हमदर्द, दीन के रक्षक और अख़लाक़ एवं इनसाफ़ के अलमबरदार की हैसियत से उनकी महानता बढ़ गई थी। मुस्लिम समाज में आलिमों को जो उच्च स्थान प्राप्त है वह इन ही सब बातों के कारण है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है— “उमवियों के अत्याचार के बाद भी आलिमों की सत्य-प्रियता की जितनी मिसालें उस ज़माने में मिलती हैं उतनी बाद के किसी ज़माने में नहीं मिलती।
फिर भी उमवी हुक्मरानों में सिर्फ़ ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ नहीं थीं और वे दुनिया के दूसरे हुक्मरानों के मुक़ाबले में निम्न या बुरे नहीं थे। वह निजी तौर पर ठीक वैसे ही थे जैसे दुनिया के दूसरे बादशाह होते हैं। उनके ज़माने में यदि हमें ख़राबियाँ नज़र आती हैं तो इसका कारण यह नहीं था कि वे निजी तौर पर अच्छे मुसलमान नहीं थे या दीन पर उनकी आस्था मज़बूत नहीं थी, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। उनके ज़माने की ख़राबियाँ दरअसल मुलूकियत (राजतन्त्र) की दमनकारी शासन प्रणाली की ख़राबियाँ थीं। वरन् उन्होंने इससे ज़्यादा कोई बुरा काम नहीं किया जो हर बादशाह करता रहता है। वैयक्तिक आधार पर अधिकतर उमवी हुक्मराँ अच्छे चरित्र के मालिक थे और इस्लामी आदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। शराब और ऐशपसंदी उनमें अभी उतना आम नहीं हुई थी जितनी बाद के हुक्मराँ में हो गई थी। उमवी हुक्मराँ आम तौर पर इस कारण ज़्यादा बदनाम हुए कि उनके दौर के इतिहास अब्बासी हुक्मरानों के दौर में लिखे गए जो उमवी ख़ानदान के कट्टर दुश्मन थे। इसके अलावा बहुत-सी ऐसी चीज़ें भी इतिहास में जगह पा गईं जो शीआने अली ने बयान किए थे, जो बनी उमय्या के राजनीतिक प्रतिद्वन्दी थे।
सल्तनत की शासन व्यवस्था
उमवी दौर में इस्लामी ख़िलाफ़त क्षेत्रफल के लिहाज़ से बड़ी विशाल हो गई थी। इतनी विशाल सल्तनत अब तक दुनिया में किसी क़ौम ने क़ायम नहीं की थी। ईरानियों और रूमियों की सल्तनतें अपने चरम उत्कर्ष के ज़माने में भी इतनी विशाल नहीं थीं। उमवी सल्तनत भी ख़िलाफ़ते राशिदा की तरह विभिन्न प्रान्तों में बँटी थी जिनका हाकिम या गवर्नर 'वाली' या 'आमिल' कहलाता था। पूरब में कूफ़ा के वाली को और पश्चिम में मिस्र के वाली को इस लिहाज़ से विशेष महत्त्व प्राप्त था कि उनकी हैसियत गवर्नर की नहीं बल्कि गवर्नर-जनरल की थी। पूरब के सारे इलाक़े ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान और सिन्ध कूफ़ा के वाली के अधीन होते थे और वही उन इलाक़ों के लिए गवर्नर मुक़र्रर करता था। अतः सिन्ध और तुर्किस्तान कूफ़ा के वाली हज्जाज बिन यूसुफ़ ही की कोशिशों से फ़तह किए गए। इसी प्रकार पश्चिम में सम्पूर्ण उत्तरी अफ़्रीक़ा और कुछ मामलों में अंदलुस (स्पेन) भी या तो मिस्र के वाली के अधीन होते थे या उत्तर पश्चिम अफ़्रीक़ा के वाली के अधीन जिसका केन्द्र क़ैरवान था। मूसा बिन नुसैर, जिनकी कोशिशों से अंदलुस इस्लामी सल्तनत का एक हिस्सा बना, उत्तर पश्चिमी अफ़्रीक़ा के वाली थे।
उमवी दौर में बढ़ती हुई ज़रूरतों के तहत कई नए ओहदे (पद) भी क़ायम किए गए, अतः केन्द्रीय हुकूमत के निम्नलिखित चार ओहदे बुनियादी महत्त्व रखते थे—
1. किताबत :- इसका संचालक 'कातिब' कहलाता था। ख़लीफ़ा की डाक खोलना, उसकी तरफ़ से फ़रमान जारी करना और मोहरें लगाना कातिब का काम होता था। कातिब मौजूदा दौर का चीफ़ सेकरेट्री था।
2. हाजिब :- यह बिलकुल नया ओहदा था और अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में क़ायम किया गया था। कातिब बादशाह और गवर्नरों के बीच तहरीरी वास्ता (लिखित माध्यम) था और हाजिब वैयक्तिक माध्यम था। हाजिब की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति ख़लीफ़ा तक नहीं पहुँच सकता था।
3. क़ाज़ी :- यह शोब-ए-क़ज़ा यानी अदालत का संचालक होता था।
4. साहिबुल-बरीद :- यानी पोस्टमास्टर जनरल। यह डाक विभाग का संचालक होता था। यह भी एक नया विभाग था जो अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ायम किया था। उनके बाद उमवी ख़लीफ़ा ने इसे और व्यापक बनाया।
इनके अलावा दूसरे विभाग लगभग वही थे जो ख़िलाफ़ते राशिदा में थे। हाजिब के अलावा दूसरे तमाम ओहदे प्रान्तों और ज़िलों में भी मौजूद थे और गवर्नर के अधीन होते थे।
सुरक्षा व्यवस्था
मुसलमानों की फ़ौजी बरतरी ख़िलाफ़ते राशिदा की तरह बनी उमय्या के दौर में भी क़ायम रही। चीन के अतिरिक्त दुनिया का कोई देश ख़िलाफ़ते इस्लामिया के बराबर बड़ी फ़ौज मैदाने जंग में नहीं ला सकता था। सिन्ध में हालाँकि एक ही युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह हज़ार और अंदलुस में तीस हज़ार फ़ौज से ज़्यादा मैदाने जंग में लाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन तुर्किस्तान, एशिया-ए-कोचक और उत्तरी अफ़्रीक़ा की जंगों में इससे ज़्यादा फ़ौजों ने हिस्सा लिया। इस दौर में मुसलमान आसानी से दो लाख, बल्कि उससे ज़्यादा फ़ौज के साथ मैदाने जंग में आ सकते थे। फ़ौज ख़िलाफ़ते राशिदा के मुक़ाबले में ज़्यादा बेहतर असलहों से लैस हो गई थी और फ़ौजी संगठन भी पहले के मुक़ाबले में अब बेहतर था। मुसलमानों के पास आधुनिक हथियारों की अब समय के अनुसार कोई कमी नहीं थी।
जल-सेना में भी इस दौर में काफ़ी विकास हुआ। शाम, मिस्र और तूनिस (Tunish) में जहाज़ बनाने के कारख़ाने खोले गए जो 'दारुल सनाआ' कहलाते थे। इस दौर में रूम सागर में मुसलमान सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बन चुके थे। क़बरस (Cyprus), रोदस (Rhodes) और बिलयालक के टापू फ़तह किए गए और सक़लिया, सरदानिया और यूनान के विभिन्न हिस्सों पर लगातार समुद्री हमले किए गए। सुलैमान के ज़माने में क़ुस्तनतीनिया पर मुसलमानों ने जो हमला किया था उसमें एक हज़ार आठ सौ जहाज़ इस्तेमाल किए गए थे। इससे पहले दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी समुद्री मुहिम में इतनी बड़ी तादाद में जहाज़ों ने हिस्सा लिया हो।
सांस्कृतिक विकास
बनी उमय्या का दौर आर्थिक ख़ुशहाली का ज़माना था। पूरब के वे तमाम इलाक़े जो इस्लामी जीतों से पहले ईरानियों और रूमियों की निरन्तर जंगों के कारण उजड़ गए थे, एक बार फिर आबाद हो गए। सौ साल की शान्तिपूर्ण और मज़बूत हुकूमत के नतीजे में खेती-बाड़ी और उद्योग-धन्धे का विकास हुआ। कूफ़ा [उमवी दौर में कूफ़ा में अस्सी हज़ार से ज़्यादा घर थे। दूसरे शब्दों में कूफ़ा की आबादी चार लाख से ज़्यादा थी जो उस ज़माने के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा थी। बसरा भी कूफ़ा के बराबर था। सोलह वर्ग-मील में फैला हुआ था और चारों ओर नहरों का जाल था। अपनी हरियाली के कारण बसरा का इलाक़ा इस्लामी दुनिया के चार बहुत ख़ूबसूरत इलाक़ों में गिना जाता था।], बसरा और फ़िस्तात के शहर जिनकी बुनियाद ख़िलाफ़ते राशिदा में पड़ी थी, अब सल्तनत के सबसे बड़े शहर बन चुके थे। दमिश्क़, स्कंदरिया, अस्फ़हान, रै और नेशापुर के शहरों का और विस्तार किया गया। उत्तरी अफ़्रीक़ा में क़ैरवान की बुनियाद पड़ी जो दूसरी शताब्दी (हिजरी) के प्रारंभ तक इस क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा एवं इस्लामी सभ्यता का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया था। फ़िलस्तीन में रमला, ईरान में शीराज़ और सिन्ध में मनसूरा और महफ़ूज़ा के नए शहर आबाद हुए।
राजधानी दमिश्क़ एक विशाल एवं विस्तृत मरुद्यान में स्थित थी। झीलों और बाग़ों की बहुतायत के कारण यह शहर और इसके आस-पास का इलाक़ा उस ज़माने में इस्लामी दुनिया के चार बहुत ख़ूबसूरत इलाक़ों में गिने जाते थे। उमवी दौर में महलों और शानदार इमारतों की अधिकता के कारण शहर की रौनक़ में चार चाँद लग गए थे। यहाँ की जल आपूर्ति की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। झीलों का पानी खुली और बन्द नालियों के ज़रिए हर घर में पहुँचा दिया गया था और हर बड़े घर के आंगन में फ़व्वारे लगे हुए थे।
सांस्कृतिक विकास जीवन के हर विभाग में हुआ। और यदि इमारतें एक मुल्क की ख़ुशहाली और दौलतमंदी का सुबूत होती हैं तो फिर उमवी दौर में बननेवाली इमारतें उस दौर की ख़ुशहाली की गवाही देती हैं। अब ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर की सादा इमारतों की जगह पक्की और शानदार इमारतों ने ले ली। उस ज़माने की यादगार इमारतें या तो मस्जिदों की शक्ल में वुजूद में आईं जो इबादतगाहों के साथ शैक्षिक उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल होती थीं या शाही महलों की शक्ल में। इन इमारतों के निर्माण में पहली बार रूमी, शामी, ईरानी और हिन्दुस्तानी कारीगरों ने मिलकर काम किया और इस प्रकार एक नए निर्माण कला की बुनियाद पड़ी। उमवी दौर की प्रारंभिक इमारतें अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से सम्बन्ध रखती हैं।
उमवी हुकूमत का केन्द्र दमिश्क़ था जो न केवल दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से था, बल्कि एक ऐसे इलाक़े में स्थित था जो उस ज़माने में सभ्यता एवं संस्कृति का केन्द्र था। अरब अभी सांस्कृतिक लिहाज़ से पिछड़े हुए थे, जिसके कारण अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) को यह एहसास परेशान रखता था कि रूमी और शामी (सीरियाई) बाशिन्दे मुसलमानों को असभ्य और अपने से हीन न समझें। अतः उन्होंने इस हीन भावना के ख़ात्मे के लिए वह संस्कृति अपनानी चाही जो उस दौर की विकसित संस्कृति समझी जाती थी। अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) की इन भावनाओं की अभिव्यक्ति ख़िलाफ़ते राशिदा के ज़माने से ही होनी शुरू हो गई थी, जिसकी चर्चा हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शाम के दौरे के सिलसिले में पिछले एक अध्याय में की जा चुकी है।
अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने रूमी संस्कृति के जिन पहलुओं को अपनाया, उनमें एक निर्माण कला भी है। उनके दौर में पक्की इमारतें और आलीशान महल बनना शुरू हुए। वे अपनी नव निर्मित इमारतों के बारे में लोगों की राय भी मालूम करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और रूमी राजदूत से उन्होंने इस विषय पर जो बात की उसकी चर्चा की जा चुकी है। रूमी राजदूत के जवाब के बाद अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मिट्टी की जगह पत्थरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और धीरे-धीरे संगमरमर और मोज़ैक का इस्तेमाल भी शुरू हो गया जिसको उस ज़माने में 'फ़ुसैफ़साअ' कहा जाता था। महलों के अतिरिक्त अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में बसरा, कूफ़ा और फ़िस्तात (मिस्र) में पक्की और शानदार मस्जिदें बनाई गईं। बसरा की जामे-मस्जिद और दारुल-अमारत वहाँ के गवर्नर ज़ियाद ने बनवाए थे। बसरा की इस मस्जिद को यह प्रधानता प्राप्त है कि इसमें पहली बार पत्थर के स्तंभ इस्तेमाल किए गए और एक मीनार भी था जो संभवतः इस्लामी दुनिया का पहला मीनार था। कूफ़ा की जामे-मस्जिद भी ज़ियाद ने एक ईरानी कारीगर से बनवाई थी। इसमें साठ हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ सकते थे। मिस्र में जामे अम्र बिन आस को अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में विस्तृत किया गया और इसमें चार मीनार बढ़ाए गए।
उमवी दौर के निर्माण-कला का पहला शाहकार क़ुब्बतुस-सख़रा है, जो अब्दुल मलिक के ज़माने में बैतुल मक़्दिस में बनाया गया था। मुसलमानों की निर्माण कला का यह सबसे अच्छा और सबसे पहला नमूना है जो आज भी मौजूद है।
वलीद का दौर निर्माण कला का सुनहरा दौर था। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी इमारतें बनाई गईं। वलीद के ज़माने में भवन निर्माण की अभिरुचि इतनी आम हो गई थी कि जब लोग आपस में मिलते थे तो उनकी बात-चीत का सबसे बड़ा विषय भवन निर्माण ही होता था। उस ज़माने में दमिश्क़ में शाही ख़ानदान के लोग, सरदारों और धनवानों ने बहुलता से शानदार इमारतें बनवाईं। उस दौर की सबसे शानदार इमारतें दमिश्क़ की जामे उमवी और मदीना की मस्जिदे नबवी हैं, जिनकी चर्चा वलीद के दौर में की जा चुकी है। जामे उमवी में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था और दीवारों में लाजवरदी (एक प्रकार का नीला पत्थर) का काम किया गया था। मस्जिद में रौशनी के लिए छः सौ क़ंदीलें सोने की ज़ंजीरों से लटकी थीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ज़माने में सोने-चाँदी के इस इस्तेमाल को फ़ुज़ूलख़र्ची समझकर तमाम क़ीमती सामान निकलवाकर बैतुलमाल में दाख़िल कराने का इरादा कर लिया था। इत्तिफ़ाक़ से उसी ज़माने में एक रूमी राजदूत दमिश्क़ आया हुआ था। उसने जामे मस्जिद को देखकर कहा—
"हम लोग समझते थे कि मुसलमानों का उत्थान कुछ दिनों का है, लेकिन इस इमारत को देखकर अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान एक ज़िन्दा रहनेवाली क़ौम है।"
रूमी राजदूत की यह राय सुनने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपना इरादा स्थगित कर दिया।
सामाजिक जीवन
शस्त्र-निर्माण, जहाज़-निर्माण, वस्तु-निर्माण और बरतन-निर्माण उस ज़माने के विशेष उद्योग-धन्धे थे। हिशाम के दौर में रेशमी कपड़े के उद्योग ने विशेषकर तरक़्क़ी की थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि जिस प्रकार वलीद के दौर में लोगों की बातचीत का विषय इमारतें और उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रहमतुल्लाह अलैह) के दौर में दीनी बातें होती थीं, उसी प्रकार हिशाम के दौर में बातचीत का विषय लिबास और कपड़े होते थे। समाज की ख़ुशहाली का कारण अच्छा लिबास धारण करना आम बात थी। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा), जिनका सम्बन्ध प्रारंभिक काल से है, कहती थीं कि उनके पास एक क़ीमती दुपट्टा था। जब मदीना में किसी लड़की की शादी होती थी तो औरतें दुल्हन के लिए यह दुपट्टा ले जाती थीं, परन्तु अब मेरी लौण्डी भी इसे ओढ़ना पसंद नहीं करेगी। उमवी दौर के आख़िर में अच्छा लिबास पहनना समाज का आवश्यक अंग बन गया था। उस दौर के आलिम भी, जिनकी ज़िंदगी में इबादत और सादगी का ज़ोर होता था, अच्छा लिबास पहनते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम हसन बसरी, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैहिम) सब अच्छा लिबास पहननेवाले थे। इमाम मालिक से जब किसी ने सवाल किया कि आप आलिम होकर इतना क़ीमती लिबास क्यों पहनते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे ज़माने में आलिमों का यही तरीक़ा है।
हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हालात में इस वाक़िआ का ज़िक्र किया जा चुका है कि जब मदाइन की फ़तह के बाद ईरान का ख़ज़ाना और शाही सामान मदीना पहुँचा तो हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) उसे देखकर रो पड़े थे, क्योंकि उसमें उन्हें मुसलमानों के पतन की निशानियाँ नज़र आती थीं। उमवी दौर में यह निशानियाँ और स्पष्ट हो गईं। इस्लामी ख़िलाफ़त की सीमाओं में आबाद लोगों में से अधिकतर मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उनकी तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक़ पूरी तरह नहीं हो सकी थी। तरबियत का यह फ़र्ज़ (कर्त्तव्य) सिर्फ़ आलिमों तक ही सीमित रह गया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के दौर को छोड़कर हुकूमत ने इस मामले में कभी उस भावना के तहत काम नहीं किया जो ख़िलाफ़ते राशिदा की विशेषता थी। शासक वर्ग अपने निजी स्वार्थों को इस्लाम के उच्च उद्देश्यों पर प्रधानता देने लगा। नतीजा यह हुआ कि नव मुस्लिम नागरिक बहुत-से पुराने परन्तु ग़ैर इस्लामी आस्थाओं, दृष्टिकोणों, अंधविश्वासों और जीवन गुज़ारने के तरीक़ों को भी अपने साथ ले आए जो मुस्लिम समाज के अंग बन गए। अतः उस दौर के समाज एवं संस्कृति में कई ऐसी नई बातें नज़र आती हैं जो इस्लामी आत्मा के विपरीत हैं और जो मात्र धन की अधिकता, दमनकारी शासन-प्रणाली और सैद्धान्तिक तरबियत की कमी के कारण मुस्लिम समाज में घुस आईं और इस प्रकार उस पतन का रास्ता साफ़ हो गया जिसका संकेत हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने किया था।
रूमी और ईरानी प्रभावों के तहत दरबारों में ख़्वाजा-सराओं (नपुंसक व्यक्ति) का लज्जाजनक रिवाज शुरू हो गया। बड़े-बड़े 'हरम' वुजूद में आए जो कनीज़ों और लौंडियों से भरे हुए थे। इसमें शराब, संगीत और नृत्य को पहली बार सांस्कृतिक मरतबा मिला। महलों की सजावट में चित्रकारी से भी काम लिया गया। हालाँकि ये सब ख़राबियाँ बहुत सीमित थीं और आम मुस्लिम समाज इनसे पाक रहा, लेकिन इनके कारण संस्कृति और ललित कलाओं के इस्लामी आधार पर विकसित होने में सख़्त रुकावट पड़ी। वेश्यावृत्ति अभी तक मुस्लिम समाज में दाख़िल नहीं हुई थी और एक मुसलमान औरत के तवायफ़ होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अतः इस्लामी सल्तनत में वेश्यालय नहीं था, हालाँकि यह बुराई ग़ैर इस्लामी दुनिया में हमेशा की तरह उस वक़्त भी आम थी।
संगीत को संरक्षण मिलना दरबार से शुरू हुआ और धीरे-धीरे इसने उन सरदारों के घरों में भी जगह पा ली जो मज़हबी रुझान नहीं रखते थे। कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में संगीत को जिस व्यक्ति ने रिवाज दिया उसका नाम 'ताऊस' था। अब दरबार गाने-बजानेवालों का केन्द्र बन गया। गानेवाले और गानेवालियाँ आम तौर पर ईरानी या ग़ैर अरब होती थीं। वाद्य-यन्त्र भी ज़्यादातर ग़ैर अरब क़ौमों से लिए गए। नृत्य एवं संगीत का उद्देश्य मात्र मनोरंजन, ऐश एवं मानसिक तृप्ति था। इसलिए इन चीज़ों ने धीरे-धीरे मुस्लिम समाज में यौन विकृति और ऐयाशी का रास्ता खोला।
हसन बसरी (रहमतुल्लाह अलैह) कहा करते थे—
"बसरा की रौनक़ मुनाफ़िक़ों के दम से है, अगर मुनाफ़िक़ न रहें तो शहर में लोगों का मन लगना मुश्किल हो जाए।"
यह कहते समय शायद उनके मन में यही नई संस्कृति थी जो मुसलिम समाज में जगह पकड़ रही थी।
इस्लामी इतिहास में मुसलमानों का पतन मुलूकियत (राजतन्त्र) और ग़ैर इस्लामी संस्कृति के रास्ते शुरू हुआ।
मुसलमान औरतें इस्लामी निर्देश के मुताबिक़ परदा करती थीं, लेकिन यह परदा अभी इतना सख़्त नहीं हुआ था जितना बाद के ज़माने में उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हो गया। औरतें ज़रूरी कामों एवं मनोरंजन के लिए बाहर निकलती थीं और ज्ञान-विज्ञान की गोष्ठियों में सम्मिलित होती थीं। परन्तु यह गोष्ठियाँ औरतों-मर्दों की मिली-जुली नहीं होती थीं, बल्कि औरतें आम तौर पर परदे के पीछे बैठती थीं। जस्टिस अमीर अली ने अपनी तारीख़े इस्लाम में और दूसरे इतिहासकारों ने ज्ञान-विज्ञान की गोष्ठियों में मर्दों-औरतों के शामिल होने से यह ग़लत नतीजा निकाल लिया है कि उमवी दौर में औरतें परदा नहीं करती थीं और मिली-जुली सोसाइटियों में शामिल होती थीं और यह कि औरतों की अलग गोष्ठियों का रिवाज वलीद द्वितीय के ज़माने में हुक्मरान की अनैतिक हरकतों के कारण हुआ। मौलाना शिबली नोमानी ने अमीर अली की इस ग़लत बात का खण्डन किया है।
उमवी दौर की प्रतिष्ठित औरतों में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) और मशहूर बुज़ुर्ग औरत राबिया बसरी के नाम ज़िक्र के क़ाबिल हैं। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की चर्चा पिछले पृष्ठों में की जा चुकी है। इस दौर की एक और प्रसिद्ध औरत सकीना बिन्त हुसैन थीं जो अपनी सुन्दरता के अलावा ज्ञान-विज्ञान, शेर और संगीत की महफ़िलों की रौनक़ थी।
ज्ञान-विज्ञान
आम तौर पर यह समझा जाता है कि मुसलमानों में ज्ञान-विज्ञान का विकास अब्बासी दौर से शुरू हुआ, लेकिन हक़ीक़त यह है कि मुसलमानों में ज्ञान-विज्ञान का प्रारंभ उमवी दौर ही में शुरू हो गया था और अब्बासी दौर में इसको तरक़्क़ी मिली। इसी तरह मुसलमानों में ज्ञान-विज्ञान की गतिविधियों का असल प्रेरक इस्लाम था, यूनानी ज्ञान उन गतिविधियों का प्रेरक नहीं था जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है।
ज्ञान-प्राप्ति पर इस्लामी शिक्षाओं में बहुत ज़ोर दिया गया है। क़ुरआन में कहा गया है—
“तुममें से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया अल्लाह उनके दर्जे बुलन्द करेगा।” (अल-मुजादला)
प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी ज्ञान-प्राप्ति के महत्त्व पर बार-बार ज़ोर देते थे। अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित हदीसें बहुत महत्त्व रखती हैं :
(1) इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।
(2) इल्म ख़ज़ाना है और उसकी चाभी सवाल है।
(3) आबिद (इबादत करनेवाले) पर आलिम (विद्वान) की श्रेष्ठता ऐसी ही है जैसे कि मुझे तुममें से सबसे मामूली आदमी पर श्रेष्ठता प्राप्त है। (तिरमिज़ी)
(4) जिस व्यक्ति ने एक रास्ता इल्म प्राप्त करने के लिए तय किया वह जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला। (बुख़ारी)
क़ुरआन और हदीस में ज्ञान-प्राप्ति के आग्रह के अलावा ख़ुद इस्लामी शिक्षाओं को समझने के लिए भी विभिन्न ज्ञान का हासिल करना ज़रूरी था। उदाहरणत: 'सर्फ़ व नह्व' (व्याकरण) और शब्द और ज्ञान की बुनियाद इसलिए पड़ी कि उसके बिना क़ुरआन के अर्थ को नहीं समझा जा सकता था। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने क़ुरआन पढ़ानेवालों को शब्द-ज्ञान का ज्ञाता होना ज़रूरी क़रार दिया। इस बात ने अरबी भाषा के रिसर्च के लिए रास्ते खोले। इन ही कारणों से हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके शागिर्द अबुल असवद दूइली ने इल्मे नह्व के प्रारंभिक उसूल प्रतिपादित किए। 'इल्मे तफ़सीर' की बुनियाद इसलिए पड़ी कि क़ुरआन में ज्ञान-विज्ञान के जो मोती हैं उनकी व्याख्या की जाए। हदीसें इसलिए संकलित की गईं कि क़ुरआन की शिक्षाओं, रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेशों और उनकी ज़िन्दगी को पूरी तरह समझा जा सके। इल्म फ़िक़्ह (इस्लामी विधिशास्त्र) की बुनियाद इसलिए पड़ी कि इस्लामी क़ानून को व्यवस्थित एवं संकलित रूप में पेश किया जाए। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन-चरित्र को सुरक्षित करने और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के हालात को लिखित रूप में लाने के शौक़ ने इतिहास और जीवनी-लेखन जैसी विद्या की बुनियाद डाली। ज़कात, मीरास, जिज़्या और ख़िराज की समस्याएँ सुलझाने के लिए गणित जानना ज़रूरी था। हदीसें एकत्र करनेवालों ने हदीसों की तलाश और प्राप्ति के लिए दूर-दूर के सफ़र किए। हज की अदायगी के लिए इस्लामी दुनिया के कोने-कोने से लोगों के क़ाफ़िले मक्का का रुख़ करने लगे और इस बात ने पर्यटन का शौक़ पैदा किया, और इस प्रकार भूगोल-शास्त्र की बुनियाद पड़ी। चिकित्सा-विज्ञान एक स्वाभाविक ज़रूरत थी और उसकी ओर इस स्वाभाविक ज़रूरत के अलावा इस कारण भी ध्यान दिया गया कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसकी हौसला अफ़ज़ाई की थी।
कहने का अर्थ यह है कि मुसलमानों में ज्ञान-विज्ञान की सरगर्मी ख़ुद इस्लाम के कारण शुरू हुई। इसके विकास में न हुक्मरानों का हाथ था न ग़ैर मुस्लिम क़ौमों के दृष्टिकोणों का। मुसलमानों ने ग़ैर मुस्लिम स्रोत से फ़ायदा ज़रूर उठाया, परन्तु वे पर्याप्त नहीं थे। यही कारण है कि उमवी दौर में ज्ञान-विज्ञान की तरक़्क़ी हुकूमत की सरपरस्ती पर निर्भर नहीं थी। यह ज्ञान-विज्ञान का एक स्वतन्त्र आन्दोलन था और इसके असल संचालक 'सहाबा' और 'ताबिईन' थे जो अधिकतर हुकूमत के प्रभाव से आज़ाद थे। शैक्षणिक सरगर्मियों की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि हदीस का ज्ञान जिन सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से प्राप्त किया गया, उनकी तादाद दस हज़ार थी। फिर हर सहाबी (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अनगिनत शागिर्द छोड़े। उदाहरणत: हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शागिर्दों की तादाद आठ सौ के लगभग थी। जीवनियों की मशहूर किताब 'तबक़ात इब्ने साद' में कुछ प्रमुख शहरों के जिन 'ताबिईन' के हालात मिलते हैं, उनकी तादाद एक हज़ार एक सौ बानवे (1192) है। इनमें से 484 मदीना से, 131 मक्का से, 413 कूफ़ा से और 164 बसरा से सम्बन्ध रखते थे। और ये सब ज्ञान-विज्ञान के मामले में इतने प्रतिष्ठित थे कि इनके हालात लिखने की ज़रूरत महसूस की गई।
उमवी दौर को ज्ञान-विज्ञान के लिहाज़ से दो भागों में बाँटा जा सकता है—
प्रारंभिक दौर जिसमें सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) शिक्षक होते थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा), हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) इस दौर के प्रसिद्ध आलिम (गुरु) थे। अधिकतर हदीसें इन्हीं बुज़ुर्गों के ज़रिये हम तक पहुँचीं।
दूसरा दौर वह है जिसमें ताबिईन ने शिक्षक के कर्त्तव्य निभाए। यह सूची बहुत लम्बी है, हम यहाँ सिर्फ़ कुछ प्रसिद्ध ताबिईन की चर्चा करेंगे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—
1. सईद बिन मुसय्यब (रहमतुल्लाह अलैह) (14 हि०/635 ई० से 94 हि०/712 ई०) - हदीस और इस्लामी विधान के ज्ञाता थे। 'सैयदुत-ताबिईन' कहलाते थे। शेरो-शायरी का भी बड़ा शौक़ था।
2. उरवह बिन ज़ुबैर (रहमतुल्लाह अलैह) (23 हि०/643 ई० से 94 हि०/712 ई०) - अहदे रिसालत की जंगों के इतिहास पर सबसे ज़्यादा ज्ञान रखते थे।
3. हसन बसरी (रहमतुल्लाह अलैह) (20 हि०/640 ई० से 110 हि ०/728 ई०) - ज्ञान के सागर थे। उनकी तक़रीरें (भाषण) उत्कृष्ट साहित्य का नमूना हैं। तसव्वुफ़ (अध्यात्मवाद) उनका विशेष विषय था और तसव्वुफ़ के तमाम सिलसिले आपके ज़रिये ही हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) तक पहुँचते हैं।
4. मुजाहिद बिन ज़ुबैर (रहमतुल्लाह अलैह) (21 हि०/641 ई० से 102 हि०/720 ई०) -हदीस और फ़िक़्ह के इमाम थे। अपने समय के एक बहुत बड़े पर्यटक थे।
5. शाबी (रहमतुल्लाह अलैह) (19 हि०/640 ई० से 104 हि०/722 ई०) — क़ुरआन, हदीस और फ़िक़्ह (इस्लामी विधान) के अलावा अहदे रिसालत की जंगों के इतिहास के ज्ञाता थे। गणित, साहित्य और शायरी में भी निपुण थे।
6. इमाम ज़ुहरी (रहमतुल्लाह अलैह) (50 हि०/670 ई० से 124 हि०/741 ई०) — अपने दौर के सबसे बड़े लेखक थे। मदीना के एक-एक घर में जाकर मर्दों और औरतों से हदीसें और सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की कही बातें जमा कीं और उन्हें लिखित रूप दिया।
7. क़तादा (रहमतुल्लाह अलैह) (61 हि०/680 ई० से 117 हि०/735 ई०) - तफ़सीर और हदीस के अलावा लुग़त (शब्दकोश) और अरब के इस्लाम-पूर्व इतिहास के विशेषज्ञ थे।
8. मकहूल (रहमतुल्लाह अलैह) (मृत्यु 118 हि०/736 ई०) – फ़िक़्ह (इस्लामी विधान) की प्रथम दो किताबों के लेखक, हदीस की तलाश के लिए लम्बा सफ़र किया।
9. यज़ीद बिन हबीब (रहमतुल्लाह अलैह) (53 हि०/672 ई० से 118 हि०/736 ई०) - मिस्र के क़ाज़ी और इतिहास के विशेषज्ञ।
10. हम्मादुर-राहुविया - अरबों के प्राचीन इतिहास, शजरा (वंशावली) और अशआर (कविताओं) के विशेषज्ञ।
11. ईसा बिन उमर नहवी (मृत्यु 147 हि०/764 ई०) - अरबी व्याकरण के सूत्रधार ख़लील और सीबवैह के गुरु थे।
इनके अलावा प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ख़ानदान के तीन बुज़ुर्ग इमाम ज़ैनुल अबिदीन, इमाम बाक़र और इमाम जाफ़र (रहमतुल्लाह अलैहिम) भी इसी दौर से सम्बन्ध रखते थे। उनका घर मदीना में एक बड़े अध्ययन-कक्ष की हैसियत रखता था।
क़ुरआन की 'क़िरअत' (पढ़ना) एक अलग विद्या है और इसकी बुनियाद जिन सात क़ारियों [सात क़ारियों के नाम ये हैं :-
(i) अबू अब्दुर्रहमान नाफ़े (मृत्यु - 169 हि०/785 ई०, मदीना)
(ii) अबू माबद अब्दुल्लाह (मृत्यु - 120 हि०/737 ई०, मक्का)
(iii) अबू उमर बिन अला (मृत्यु - 154 हि०/770 ई०, बसरा)
(iv) अबू इमरान अब्दुल्लाह (मृत्यु - 118 हि०/736 ई०, दमिश्क़)
(v) अबू बक्र आसिम (मृत्यु - 127 हि०/744 ई०, कूफ़ा)
(vi) अबू अम्मरा हमज़ा (मृत्यु - 157 हि०/773 ई०, कूफ़ा)
(vi) अबुल हसन अली (मृत्यु - 189 हि०/805 ई०, कूफ़ा) —तारीख़े अफ़कारो उलूमे इस्लामी, पृ०- 182-187] पर है, वे भी उसी दौर में थे और 'क़ुर्रा-ए-सबआ' कहलाते थे।
यह सही है कि उमवी दौर में ज्ञान-विज्ञान की इन सरगर्मियों के बावजूद पुस्तक लिखने तथा संपादन का ज़्यादा रिवाज नहीं हुआ था। लोग स्मरण शक्ति (हाफ़िज़ा) को लिखी हुई चीज़ों पर तरजीह देते थे और लिखी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद भी यह हक़ीक़त है कि इस्लामी इतिहास में पुस्तक लिखने का बाक़ायदा प्रारंभ भी उसी दौर में हुआ। तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह, इतिहास और चिकित्सा पर किताबें लिखी और अनुवाद की गईं। हालाँकि उनमें से अधिकतर किताबें उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु अब्बासी दौर में इन विषयों पर जो किताबें लिखी गईं उनकी बुनियाद उमवी दौर की इन्हीं किताबों और लेखों पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) और मुजाहिद बिन ज़ुबैर ने क़ुरआन की जो तफ़सीर की थी वे अब किताबी शक्ल में उपलब्ध हैं। उरवा बिन ज़ुबैर ने फ़िक़्ह पर कई किताबें लिखीं और मग़ाज़ी (युद्धों एवं योद्धाओं का विषय) एवं सीरत (जीवनी) पर पहली किताब लिखी। इमाम ज़ुहरी (रहमतुल्लाह अलैह) कई किताबों के लेखक थे और उनके फ़तवे तीन वृहत् भागों में जमा किए गए थे। हम्माम बिन मुनब्बह (40 हि०/660 ई० से 131 हि०/784 ई०) ने हदीसें संकलित की थीं जो 'सहीफ़ा-ए-हम्माम' के नाम से मशहूर था और अब प्रकाशित हो चुका है। हदीसों के और कई संकलन प्रकाशित हुए थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के हुक्म पर इस्लामी रियासत के हर हिस्से से हदीस के संकलन तैयार करके दमिश्क़ भेजे गए थे जहाँ से उनकी नक़लें इस्लामी दुनिया के विभिन्न शहरों में भेजी गईं। इनमें केवल वे संकलन जो इमाम ज़ुहरी (रहमतुल्लाह अलैह) ने तैयार किए थे कई ऊँटों पर लादे गए थे।
ईसा बिन अम्र सक़फ़ी (मृत्यु, 147 हि०/764 ई०) ने फ़न्ने नह्व (व्याकरण-शास्त्र) पर दो किताबें लिखी थीं। एक यमनी आलिम उबैद बिन शिरया ने अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हुक्म से किताबुल-अम्साल और किताबुल-मुलूक लिखी जो अजमी (ग़ैर अरब) इतिहास पर आधारित थी। अवाना बिन हकम कल्बी ने 'किताबुत तारीख़' और 'सीरते मुआविया' लिखी। वहब बिन मुनब्बह (मृत्यु 110 हि०/728 ई०) ने यमन के बादशाहों के हालात पर किताब लिखी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने इसराईली चिकित्सक मासिर जोया से यूनानी लेखक अहरन की किताब का अरबी में अनुवाद करवाया। हिशाम ने ईरान के इतिहास और ईरानी ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित एक किताब का अनुवाद करवाया। इनके अतिरिक्त क़तादा (मृत्यु 117 हि०/735 ई०) और अबू अम्र बिन अला (मृत्यु 154 हि०/770 ई०) शब्दकोष के माहिर समझे जाते थे। भाषा और शब्दकोष के क्षेत्र में वर्षों तक अरब के रेगिस्तान की ख़ाक छानी और अपनी मेहनत के बाद जो कुछ जमा किया वह अब्बासी दौर में शब्द-कोष की तैयारी में काम आया। इसी तरह मुहम्मद बिन साइब कल्बी अनसाब (वंशज्ञान) के माहिर थे और इस ज्ञान ने बाद के ज़माने में जो उन्नति की उसका बड़ा स्रोत उन ही की रिवायत है।
पत्र लेखन एवं किसी विषय पर लेख लिखना उस दौर में एक कला समझा जाता था। उस ज़माने में इस कला को किताबत कहा जाता था और कातिब की हैसित साहित्यकार एवं लेखक की होती थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि किताबत अब्दुल हमीद से शुरू हुई और इब्नुल अमीद पर ख़त्म हुई। यह अब्दुल हमीद ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के कातिब थे और इब्नुल अमीद चौथी सदी हिजरी के साहित्यकार थे। एक उमवी शहज़ादा ख़ालिद बिन यज़ीद ने यूनानियों से चिकित्सा दर्शन और रसायन-शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और ख़ुद भी रसायन-शास्त्र पर किताबें लिखीं।
यह शैक्षिणिक-विकास (इल्मी तरक़्क़ी) जैसा कि हम बता चुके हैं उस जज़्बे का नतीजा था जो इस्लाम ने मुसलमानों में शिक्षा-प्राप्ति के लिए पैदा कर दिया था। यह एक ऐसा शैक्षणिक आन्दोलन था जिसका प्रेरक इस्लाम था और दरबारी सरपरस्ती से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं था। हुकूमत ने इस क्षेत्र में बहुत कम प्रोत्साहन दिया। शेरो-शायरी साहित्य की एक मात्र विद्या थी जिसकी इस दौर में सरकारी तौर पर सरपरस्ती की गई। अरबी ज़बान के तीन प्रमुख शायर अख़तल, फ़रज़्दक़ और जरीर उमवी दरबार से सम्बन्ध रखते थे। इनमें अख़तल ईसाई था। उमवी हुक्मरानों ने शायरी की सरपरस्ती शाहाना मिज़ाज के मुताबिक़ की जिसके कारण अरबी शायरी सही दिशा पर आगे न बढ़ सकी और उसमें इस्लाम से पहले की वही ख़राबियाँ फिर पैदा हो गईं जिन्हें रिसालत और ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में ख़त्म करने की कोशिश शुरू की गई थी। इसी प्रकार शायरों के लिए शराबी होना एक फ़ैशन बन गया था।
इसके विपरीत ज्ञान एवं साहित्य की वह दुनिया जिसपर आलिमों का वर्चस्व था, हुकूमत के मुक़ाबले में इस्लामी रूह से अधिक निकट थी और इन आलिमों के कारण उस दौर का समाज इस्लामी शिक्षाओं से ज़्यादा दूर न हो सका। आलिमों और साहित्यकारों में अरब और ग़ैर अरब दोनों शामिल थे, बल्कि उस दौर के आलिमों में ईरानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनके बीच रंग एवं नस्ल का कोई भेद बिलकुल नहीं था। इस जगह यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस दौर के ग़रीब अरब आलिमों की एक बड़ी तादाद ग़ुलामों की थी। हसन बसरी, मुजाहिद बिन जुबैर, सईद बिन जुबैर, मुहम्मद बिन सीरीन और अबू ज़न्नाद (रहमतुल्लाह अलैहिम) या तो ग़ुलाम थे या ग़ुलाम की औलाद। ग़ुलामों को ज्ञान-विज्ञान की दुनिया की सरदारी और मुसलमान अवाम की सरदारी इस्लाम की बदौलत ही नसीब हुई।
ख़िलाफ़त बनी उमय्या
41 हिजरी/661 ई० से 132 हिजरी/750 ई० तक
अमीर मुआविया - 41 हि०/661 ई० से 60/हि०/680 ई०
यज़ीद प्रथम - 60 हि०/680 ई० से 64 हि०/683 ई०
मरवान प्रथम - 64 हि०/684 ई० से 65 हि०/685 ई०
अब्दुल मलिक बिन मरवान - 65 हि०/685 ई० से 86 हि०/705 ई०
वलीद प्रथम - 86 हि०/705 ई० से 96 हि०/715 ई०
सुलैमान - 96 हि०/715 ई० से 99 हि०/717 ई०
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ - 99 हि०/717 ई० से 101 हि०/720 ई०
यज़ीद द्वितीय - 101 हि०/720 ई० से 105 हि०/724 ई०
हिशाम - 105 हि०/724 ई० से 125 हि०/743 ई०
वलीद द्वितीय - 125 हि०/743 ई० से 126 हि०/744ई०
इबराहीम - 126 हि०/744 ई० से 127 हि०/745 ई०
मरवान द्वितीय - 127 हि०/745 ई० से 132 हि०/750 ई०
फ़तह मावराउन-नहर - 86 हि०/705 ई० से 95 हि०/714 ई०
फ़तह अंदलुस (स्पेन) - 92 हि०/711 ई० से 95 हि०/714 ई०
हादसा करबला - 61 हि०/680 ई०
क़ुस्तनतीनिया पर पहला हमला - 48 हि०/668 ई०
सिन्ध की फ़तह - 92 हि०/711 ई० से 95 हि०/714 ई०
क़ैरवान की बुनियाद - 50 हि०/670 ई०
रावर की जंग - 10 रमज़ान, 92 हि०/2 जुलाई, 711 ई०
वादी-ए-लका की जंग - 92 हि०/19 जुलाई 711 ई०
अध्याय-10
बग़दाद का उत्थान-1
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जो अबुल अब्बास सफ़्फ़ाह के नाम से ज़्यादा मशहूर है, पहला अब्बासी ख़लीफ़ा है। उसकी शासन-अवधि मात्र चार साल है। उसका यह सारा समय विरोधियों को कुचलने और नई हुकूमत को मज़बूत बनाने में गुज़रा। सफ़्फ़ाह ने इराक़ में शहर अंबार को अपनी राजधानी बनाया और 134 हि०/751 ई० में उस शहर के निकट हाशमिया के नाम से नया शहर बसाया।
इतिहासकारों ने सफ़्फ़ाह की बुद्धि, विवेक और अख़लाक़ (सदाचार) की प्रशंसा की है, परन्तु उसके अत्याचार ने उसके तमाम गुणों पर पानी फेर दिया। कहा जाता है कि सफ़्फ़ाह के कहने पर अबू मुस्लिम ख़ुरासानी ने बनी उमय्या की सत्ता ख़त्म करने में छः लाख इनसानों को मौत के घाट उतार दिया। दमिश्क़ फ़तह करके अब्बासी फ़ौजों ने वहाँ क़त्ले आम किया। हज़रत अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) सहित तमाम उमवी हुक्मरानों की क़ब्रें खोद डाली गईं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक की लाश क़ब्र में सही-सलामत मिली तो उसे कोड़ों से पीटा गया। बनी उमय्या का बच्चा-बच्चा क़त्ल किया गया और उमवी सरदारों की तड़पती लाशों पर फ़र्श बिछाकर खाना खाया गया। यही कारण है कि इतिहासकारों ने अबुल-अब्बास को 'सफ़्फ़ाह' (यानी ख़ून बहानेवाला) का नाम दिया।
सफ़्फ़ाह के दौर की एक महत्त्वपूर्ण घटना जिसे मुसलमान इतिहासकारों ने महत्त्व नहीं दिया, जंगे तालास है। यह जंग राजधानी से बहुत दूर तुर्किस्तान की पूर्वी सीमा पर अरबों और चीनियों के बीच 751 ई० में हुई थी। चीनियों ने मुसलमानों की घरेलू लड़ाई से फ़ायदा उठाकर तुर्किस्तान पर क़बज़ा करने की अन्तिम बार कोशिश की थी, परन्तु इस तालास की जंग में हारने के बाद हमेशा के लिए तुर्किस्तान से हाथ धो बैठे। अरबों की फ़तह ने इस बात का फ़ैसला कर दिया कि इन मुल्कों की भावी सभ्यता एवं संस्कृति इस्लामी ही रहेगी और चीनी सभ्यता को वहाँ क़दम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मंसूर (136 हि०/754 ई० से 158 हि०/775 ई०)
हालाँकि अबुल-अब्बास सफ़्फ़ाह पहला अब्बासी ख़लीफ़ा है, परन्तु अब्बासियों का पहला प्रसिद्ध शासक उसका भाई अबू जाफ़र मंसूर है जो सफ़्फ़ाह के बाद ख़िलाफ़त की गद्दी पर बैठा। मंसूर ने बाईस साल हुकूमत की और ख़िलाफ़ते अब्बासिया की जड़ों को मज़बूत कर दिया। मंसूर बड़ा योग्य शासक था। वह विरोधियों के साथ कठोरता से पेश आता था, परन्तु आम प्रजा के लिए वह न्यायप्रिय बादशाह था। वह अपना पूरा समय प्रशासन के कामों पर ख़र्च करता था। उसने हुक्म दे रखा था कि जिसे भी हाकिमों (गवर्नरों) से कष्ट पहुँचे वह बिना रोक-टोक उससे शिकायत कर सकता है। वह स्वयं सादा जीवन व्यतीत करता था। एक बार उसकी लौंडी ने उसके शरीर पर पैबन्द लगे हुए कपड़े देखकर कहा, "ख़लीफ़ा और पैबन्द लगा हुआ कुर्ता!" मंसूर ने उसके जवाब में एक शेर पढ़ा जिसका अर्थ यह है—
"मर्द उस हालत में इज़्ज़त हासिल कर लेता है कि उसकी चादर पुरानी होती है और उसकी क़मीज़ में पैबन्द लगा होता है।"
मंसूर का एक बड़ा कारनामा बग़दाद की बुनियाद डालना है। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की राजधानी मदीना थी, बनी उमय्या की दिमिश्क़। मंसूर ने बनी अब्बास की राजधानी बनाने के लिए दजला नदी के किनारे एक नया शहर आबाद किया जो बग़दाद के नाम से मशहूर हुआ। आगे चलकर बग़दाद ने ऐसी तरक़्क़ी की कि वह दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। उसकी आबादी बीस लाख से ज़्यादा हो गई। कहा जाता है कि अपने चरम विकास के ज़माने में बग़दाद में सतरह हज़ार हम्माम (स्नानगृह), उससे ज़्यादा मसजिदें और दस हज़ार सड़कें और गलियाँ थीं।
मंसूर के ज़माने में अब्बासियों की हुकूमत अंदलुस (Andalus) को छोड़कर उन तमाम इलाक़ों में क़ायम हो गई जो बनी उमय्या के क़बज़े में थे। मंसूर ने अंदलुस पर भी क़बजा करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई और एक उमवी शहज़ादा अब्दुर्रहमान ने वहाँ बनी उमय्या की हुकूमत क़ायम कर ली।
मंसूर के काल की एक प्रमुख घटना अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का क़त्ल है। अब्बासियों की हुकूमत क़ायम कराने में अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का बहुत बड़ा योगदान था। परन्तु मंसूर ने जब देखा कि अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का प्रभाव बढ़ रहा है और उसकी सहानुभूतियाँ अब्बासियों से अधिक हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद के प्रति हैं तो उसने अबू मुस्लिम को धोखा देकर क़त्ल करवा दिया।
मंसूर के शासनकाल में कई बग़ावतें भी हुईं और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद की ओर से ख़िलाफ़त हासिल करने की कोशिशें भी हुईं। इनमें एक कोशिश मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नफ़्स ज़किया ने, जो हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में से थे, हिजाज़ में की और दूसरी उसी के क़रीब उनके भाई इबराहीम बिन अब्दुल्लाह ने की। परन्तु मंसूर ने इन तमाम बग़ावतों को दबा दिया।
मंसूर के काल में रूमियों से पुनः लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, जिनमें मुसलमानों को कामयाबी हुई और 155 हि०/772 ई० में मंसूर ने रूम के क़ैसर (बादशाह) को जिज़्या देने पर मजबूर कर दिया।
मंसूर का शासनकाल ज्ञान-विज्ञान की तरक़्क़ी के लिहाज़ से भी अग्रणी है। बनी उमय्या के समय में शिक्षा अधिकतर ज़बानी दी जाती थी और किताबें लिखने का रिवाज ज़्यादा नहीं हुआ था। मंसूर के समय में पुस्तक लेखन का काम विधिवत प्रारंभ हो गया। मंसूर को स्वयं भी शिक्षा के प्रसार में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसके दरबार में हर विषय के विद्वान एवं विशेषज्ञ जमा रहते थे और वह पहला ख़लीफ़ा है जिसने सुरयानी, यूनानी, फ़ारसी और संस्कृत में लिखी किताबों का अरबी में अनुवाद करवाया। ये किताबें आम तौर पर गणित, चिकित्सा-शास्त्र, दर्शन और खगोल-शास्त्र से सम्बन्धित थीं। ये वे विषय थे जिनसे अरब के मुसलमानों को वाक़फ़ियत नहीं थी। इस प्रकार मुसलमानों ने मंसूर के दौर में ज्ञान-विज्ञान की तरक़्क़ी की ओर एक अहम क़दम उठाया।
हालाँकि मंसूर के काल में हुकूमत ने ज्ञान एवं साहित्य की बड़े पैमाने पर सरपरस्ती की, परन्तु ज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्रों में अब भी सबसे ज़्यादा काम दरबार के दायरे से बाहर स्वतन्त्र रूप से आलिमों ने किया। अतः इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) ने हदीस की मशहूर किताब 'मुवत्ता' इस काल में लिखी। इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) ने फ़िक़्हे इस्लामी (इस्लामी शरीअ़त) को इसी दौर में लिखित रूप में तैयार किया और इसी काल में इब्ने इसहाक़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की प्रथम पूर्ण जीवनी तैयार की।
महदी (158 हि०/775 ई० से 169 हि०/785 ई०)
मंसूर के बाद उसका लड़का मुहम्मद महदी ख़लीफ़ा हुआ। महदी अपनी प्रकृति और स्वभाव में अपने बाप से भिन्न था। नरमदिल, ऐशपरस्त और रंगीन मिज़ाज था। परन्तु इसके बाद भी वह बुरे आचरणवाला इनसान नहीं था बल्कि कर्त्तव्यनिष्ठ हुक्मराँ था। उसने उन तमाम लोगों को जो मंसूर के काल में ज़ुल्म व सितम का निशाना बने थे माफ़ कर दिया और ज़ुल्म व ज़्यादती से जो माल हासिल किया गया था, वह भी वापस कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा है— “महदी सूरत और सीरत (चरित्र) दोनों लिहाज़ से अच्छा था। वह प्रजा में प्रिय था। अत्याचारों की रोकथाम, हत्या एवं रक्तपात से बचना, न्याय एवं इनसाफ़ और पुरस्कार एवं दान ने उसको प्रजा में लोकप्रिय बना दिया था।"
महदी के आदेश से मक्का, मदीना, यमन, बग़दाद और दूसरे बड़े-बड़े शहरों के बीच ऊँटों और ख़च्चरों के माध्यम से डाक व्यवस्था क़ायम की गई और पूरी सल्तनत में कुष्ठ रोगियों की देखभाल का सरकारी तौर पर इंतिज़ाम किया गया। महदी ने ख़ान-ए-काबा और मसजिदे नबवी का विस्तार भी कराया।
मंसूर के दौर में दूसरी ज़बानों से विभिन्न धर्मों की किताबों के जो अनुवाद किए गए थे उनके कारण मुसलमानों की आस्थाएँ प्रभावित होने लगी थीं और एक ऐसा वर्ग पैदा होना शुरू हो गया था जो केवल ऊपर से मुसलमान था, परन्तु अन्दर से वह इस्लाम और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद खोद रहा था। उन लोगों को इतिहासकारों ने 'ज़िंदीक़' लिखा है। महदी ने ज़िन्दीक़ियों के अक़ीदों के खण्डन और इस्लाम के पक्ष में किताबें लिखवाईं और इस प्रकार उसने इस्लामी आस्थाओं की रक्षा की।
महदी का दस वर्षीय काल हालाँकि शान्तिमय था परन्तु रूमियों से सरहदी लड़ाइयाँ उस दौर में भी जारी रहीं। ख़िलाफ़त की सरहदी फ़ौजें हर साल गर्मी के मौसम में एशिया-ए-कोचक के रूमी इलाक़ों पर हमले करती रहती थीं। ऐसे ही एक हमले में जो 165 हि०/781 ई० में किया गया था मुसलमान फ़ौजें रूम की राजधानी क़ुस्तनतीनिया तक पहुँच गई थीं और रूमी हुकूमत को सालाना ख़िराज देने का वादा कर के समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। इस हमले का नेतृत्व महदी के लड़के हारून ने किया था जो बाद में हारून रशीद के नाम से ख़लीफ़ा हुआ।
हारून रशीद (170 हि०/786 ई० से 193 हि०/809 ई०)
महदी के बाद उसका लड़का हादी [हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में कुछ लोग ख़िलाफ़त को अपना अधिकार समझते थे। उमवियों के बाद जब बनी हाशिम की दूसरी शाख़ बनी अब्बास की ख़िलाफ़त क़ायम हो गई तो हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) के समर्थक अब्बासियों के भी विरोधी बन गए। हादी के काल में इमाम हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में एक बुज़ुर्ग इदरीस हिजाज़ से निकलकर उत्तरी अफ़्रीक़ा के क्षेत्र में चले गए जो आज अल-मग़रिब या मराकश कहलाता है और यहाँ एक आज़ाद हुकूमत की बुनियाद डाली जो इदरीसी हुकूमत कहलाती है। यह हुकूमत 169 हि०/785 ई० में क़ायम हुई और 309 हि०/920 ई० तक क़ायम रही। इस हुकूमत का मुख्य स्थान (राजधानी) 'फ़ास' था जिसकी बुनियाद इदरीस ही ने डाली थी। यह हुकूमत अब्बासी ख़िलाफ़त को स्वीकार नहीं करती थी, परन्तु शीया नहीं थी। इदरीस मृत्यु के बाद जिस जगह दफ़्न हुए वह आजकल मौला-ए-इदरीस कहलाती है और मराकश का एक पवित्र तीर्थस्थल समझी जाती है।] ख़िलाफ़त की गद्दी पर बैठा, परन्तु सवा साल की हुकूमत के बाद उसका इंतिक़ाल हो गया और उसकी जगह उसका दूसरा भाई हारून तख़्त पर बैठा। हारून की उम्र उस समय मात्र 22 साल थी।

चित्र 2 :- ख़लीफ़ा हारून रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा का मक़बरा — ख़याल है कि यह मक़बरा अब्बासियों के आख़िरी दौर में तामीर हुआ था। मक्का मुअज़्ज़मा की मशहूर नहर ज़ुबैदा इसी नेक दिल मलका के हुक्म से तामीर की गई थी।
अब्बासी ख़लीफ़ाओं में सबसे अधिक प्रसिद्धि हारून रशीद को मिली। उसका 23 वर्षीय शासनकाल अब्बासी ख़िलाफ़त का सुनहरा दौर समझा जाता है। उस समय बग़दाद विकास की चरम सीमा पर था। सम्पन्नता और ख़ुशहाली आम थी और ज्ञान एवं कला की घर-घर चर्चा थी। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए हारून रशीद का दौर मिसाली हैसियत रखता है। हारून रशीद में बहुत-से गुण थे और इन गुणों में विरोधाभास भी था। एक ओर उसकी ज़िन्दगी विलासितापूर्ण थी तो दूसरी ओर वह बड़ा दीनदार, शरीअ़त का पाबन्द, ज्ञान-विज्ञान की तरक़्क़ी चाहनेवाला और आलिमों-विद्वानों को प्रोत्साहित करनेवाला था। प्रत्येक दिन सौ रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ता और एक हज़ार दिरहम ग़रीबों में बाँटता था। उसे जिहाद का शौक़ था और शहादत की तमन्ना थी। वह एक साल हज करता और एक साल जिहाद। जिस साल हज को जाता तो एक सौ आलिमों को साथ ले जाता और उनका ख़र्च ख़ुद उठाता और जिस साल हज को नहीं जाता तो तीन सौ आलिमों को अपनी ओर से हज करने के लिए भेजता।
वह आलिमों और नेक लोगों की बड़ी इज़्ज़त करता था और जब वे उसकी ग़लतियों पर टोकते या उसकी आलोचना करते तो वह बुरा नहीं मानता और अपनी ग़लतियाँ स्वीकार कर लेता था।
एक बार एक बुज़ुर्ग इब्ने समाक से हारून ने नसीहत करने को कहा। उन्होंने कहा—
“ख़ुदा से डर और इस बात पर यक़ीन रख कि कल तुझे ख़ुदा के सामने हाज़िर होना है और वहाँ जन्नत एवं दोज़ख़ में से एक मक़ाम इख़तियार करना है।"
यह सुनकर हारून इतना रोया कि दाढ़ी आँसुओं से तर हो गई। यह देखकर हारून के हाजिब (दरबान) फ़ज़ल बिन रबीअ ने कहा—
“अमीरुल मोमिनीन ख़ुदा के आदेशों को पूरा करते हैं और उसके बंदों के साथ इनसाफ़ करते हैं। इसके बदले में इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएँगे।"
इस पर इब्ने समाक (रहमतुल्लाह अलैह) ने हारून रशीद से कहा—
"अमीरुल मोमिनीन! उस दिन फ़ज़ल आपके साथ न होगा, इसलिए ख़ुदा से डरते रहिए और अपने अमल की देख-भाल कीजिए।"
यह सुनकर हारून फिर रोने लगा। इसी प्रकार एक बार एक बुज़ुर्ग फ़ुज़ैल बिन अयाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने उससे कहा—
"ऐ हसीन चेहरेवाले! तू इस उम्मत का ज़िम्मेदार है। तुझ ही से इसके बारे में पूछा जाएगा।"
हारून यह सुनकर रोने लगा और बिलकुल बुरा नहीं माना।
हारून रशीद के चीफ़ जस्टिस (क़ाज़ी) अबू यूसुफ़ थे। जिन्हें हारून ने यह कहकर नियुक्त किया था कि वह एक सच्चे और ईमानदार इनसान हैं। सल्तनत में तमाम क़ाज़ियों की नियुक्ति वही करते थे। इसके कारण अदालतों में ख़ूब न्याय होता था। मरने से पहले उन्होंने लोगों को गवाह बनाकर कहा—
"ऐ ख़ुदा! तू जानता है कि मैंने तेरे बंदों में कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया जो क़ुरआन व सुन्नत पर आधारित न हो और मैंने अपनी ज़िंदगी में हराम का एक दिरहम भी नहीं लिया और न किसी के साथ बेइनसाफ़ी और ज़्यादती की।"
क़ाज़ी साहब ख़लीफ़ा तक के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देते थे।
हारून ने क़ाज़ी साहब से एक किताब लिखवाई थी, ताकि उसमें ऐसे तरीक़े बताए जाएँ जिनसे प्रजा पर ज़ुल्म न हो सके और नजायज़ तरीक़े से उनसे महसूल (टैक्स) न वसूल किया जा सके। उनकी इस किताब का नाम 'किताबुल-ख़िराज है। जब यह किताब पूरी हो गई तो हारून रशीद इसी के अनुसार हुकूमत करने लगा।
दूसरी भाषाओं की किताबों के अरबी अनुवाद के जिस काम को मंसूर ने शुरू किया था हारून ने उसे ज़्यादा तरक़्क़ी दी और इस उद्देश्य से 'बैतुल हिकमत' के नाम से एक संस्था स्थापित की जिसमें काम करनेवाले आलिमों और अनुवादकों को बड़ी-बड़ी तनख़्वाहें दी जाती थीं।
रूमियों से चूँकि मुसलमानों की निरन्तर लड़ाइयाँ होती रहती थीं इसलिए हारून रशीद ने इस्लामी सल्तनत को रूमियों के अचानक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एशिया-ए-कोचक की सरहदों पर क़िले बनवाए और शाम (सीरिया) के समुद्री तटों के किनारे छावनियाँ स्थापित कीं। इस सिलसिले में हारून रशीद का रूम पर हमला इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। ये रूमी अब्बासी ख़िलाफ़त की इताअत करते थे और उन्हें ख़िराज देते थे। हारून रशीद के काल में रूमी बादशाह सक़फ़ोर ने न केवल ख़िराज देने से इनकार कर दिया, बल्कि हारून रशीद से पिछले सालों में वसूल किया हुआ ख़िराज वापस करने की माँग भी करने लगा। हारून ने जब उसका पत्र देखा तो ग़ुस्से से लाल-पीला हो गया और उसने जवाब में लिखा—
"ऐ रूमी कुत्ते! तू इसका जवाब सुनेगा नहीं बल्कि आँखों से देखेगा।"
यह जवाब भेजकर हारून ने एक ज़बरदस्त फ़ौज लेकर हमला किया और रूमियों को ऐसी शिकस्त दी कि वे फिर से ख़िराज देने लगे। इस अभियान के दौरान हारून ने 'क़ौनिया' और 'अनक़रह' के शहर भी फ़तह कर लिए थे।
बरामिका (आले बरमक)
अब्बासियों के काल में ख़लीफ़ाओं ने पहली बार अपनी मदद और सलाह-मशविरा के लिए वज़ीर का पद क़ायम किया। पहले बनी उमय्या के ज़माने में वज़ीर का पद नहीं था। हारून के ज़माने में यह्या और उसके बेटे फ़ज़ल और जाफ़र बड़े मशहूर वज़ीर हुए हैं। ये लोग चूँकि बरमक नामी व्यक्ति की औलाद में से थे, इसलिए बरामिका नाम से मशहूर हैं। बरामिका वंश के ऐतबार से ईरानी थे।
बरामिका से ज़्यादा दानशील और मुक्त हस्त वज़ीर इतिहास में बहुत कम हुए हैं। उनकी दानशीलता की प्रसिद्धि सारी दुनिया में फैल गई थी। वह कभी किसी की माँग रद्द नहीं करते थे। आलिम, साहित्यकारों और शायरों की मदद करते थे और ग़रीबों में अपना धन बाँटते रहते थे। उनकी दानशीलता की घटनाएँ बड़ी आश्चर्यजनक और रोचक हैं। हारून रशीद की ख़ुशक़िस्मती थी कि उसे इतने अच्छे वज़ीर मिल गए थे। उनके कारण उसकी सल्तनत को चार चाँद लग गए।
हारून को विशेषकर जाफ़र बरमकी से बहुत प्रेम था। वे कभी एक-दूसरे से जुदा नहीं होते थे। हारून रशीद का नियम था कि वह भेस बदलकर रातों को बग़दाद की सड़कों और गलियों में घूमा करता था, ताकि लोगों के हालात मालूम करे। उसके साथ जाफ़र बरमकी और एक ग़ुलाम मसरूर भी जाते थे। इन गश्तों में कभी-कभी बड़ी दिलचस्प घटनाएँ घटती थीं, जो इतिहास में दर्ज हैं, परन्तु ख़लीफ़ा और वज़ीर की यह दोस्ती हमेशा क़ायम न रह सकी और जाफ़र से नाराज़ होकर हारून ने उसे क़त्ल करा दिया। बाद में हारून इस घटना को याद करके रोया करता था और कहा जाता है कि जाफ़र के क़त्ल के बाद लोगों ने उसे कभी हँसता हुआ नहीं देखा। इतिहासकारों ने जाफ़र के क़त्ल और बरामिका के पतन के विभिन्न कारण लिखे हैं, परन्तु बरामिका के पतन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हारून रशीद को उनके असाधारण अधिकारों, जनता पर प्रभाव और जनप्रियता के कारण यह ख़तरा पैदा हो गया था कि कहीं वे लोग तख़्ते ख़िलाफ़त पर क़ाबिज़ न हो जाएँ।
अग़ालिबा
मंसूर के बाद मराकश का इलाक़ा अब्बासी ख़िलाफ़त से आज़ाद हो गया था। हारून रशीद के ज़माने में एक और इलाक़ा जो अफ़्रीक़ा कहलाता था और मौजूदा तराबुलस (Tripolis), तूनिस (Tunish) और अल-जज़ायर (Algiers) जिसमें आते हैं, वह किसी हद तक ख़ुद-मुख़तार हो गया। केन्द्रीय हुकूमत से दूर होने के कारण इस इलाक़े की शासन-व्यवस्था में कठिनाई होती थी इसलिए हारून ने यहाँ की हुकूमत स्थायी रूप से एक व्यक्ति इबराहिम बिन अग़ालिब और उसकी औलाद के हवाले कर दी। इस तरह अफ़्रीक़ा में एक नई हुकूमत की बुनियाद पड़ी, जो 'अग़ालिबा' या 'ख़ानदाने अग़ालिब' की हुकूमत कहलाती है। यह अग़लिबी हुकूमत व्यावहारिक रूप से ख़ुद-मख़तार थी, परन्तु अब्बासी ख़िलाफ़त को स्वीकार करती थी और हर साल नियमित रूप से ख़िराज दिया करती थी जो इसका सबूत था कि यह हुकूमत अब्बासी ख़िलाफ़त का एक हिस्सा है।
अग़लिबी ख़ानदान की यह हुकूमत 184 हि०/800 ई० से 296 हि०/909 ई० तक यानी एक सौ साल से ज़्यादा क़ायम रही। इसकी राजधानी क़ैरवान (Kairavan) थी जिसकी बुनियाद उक़बा बिन नाफ़े ने डाली थी। अग़लिबी ख़ानदान के शासनकाल में क़ैरवान ज्ञान एवं कला का उत्तरी अफ़्रीक़ा में सबसे बड़ा केन्द्र बन गया था। लेकिन अग़लिबी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा सक़लिया द्वीप की फ़तह और जल-सेना की तरक़्क़ी है। इस दौर में न केवल यह कि सक़लिया द्वीप जीता गया, बल्कि दक्षिणी इटली पर भी मुसलमानों का अधिपत्य हो गया। अग़लिबी हुकूमत का समुद्री बेड़ा इतना शक्तिशाली हो गया था कि पश्चिमी रूम सागर में कोई उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता था।
हारून रशीद ने 23 साल हुकूमत की। इंतिक़ाल के समय उसकी उम्र 47 साल थी।
उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अब तक यह नियम था कि एक ख़लीफ़ा के इंतिक़ाल के बाद एक ही ख़लीफ़ा तख़्त पर बैठता था, परन्तु हारून रशीद ने यह तरीक़ा बदल दिया और अपनी सल्तनत अपने दो बेटों अमीन और मामून में बाँट दी। अमीन को पश्चिमी ईरान और इराक़ से अफ़्रीक़ा तक तमाम पश्चिमी देश दे दिए और मामून रशीद को ईरान का बड़ा हिस्सा और सिंध नदी तक तमाम पूर्वी देश मिल गए। हारून की मृत्यु के बाद मामून रशीद ने ख़ुरासान के शहर मरू को और अमीन ने बग़दाद को अपनी राजधानी बना लिया।
हारून रशीद जैसे बुद्धिमान बादशाह की यह बहुत बड़ी ग़लती थी। उसने जान-बूझकर अपनी मज़बूत सल्तनत को दो हिस्सों में बाँटकर कमज़ोर कर दिया। कहावत मशहूर है कि एक देश में दो राजा नहीं हो सकते। अत: अमीन और मामून में जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बड़े पैमाने पर ख़ून-ख़राबा हुआ और कई साल तक इराक़ और उससे मिले हुए सूबों (प्रान्तों) में अशान्ति रही। परन्तु ख़ुशक़िस्मती से इस जंग में मामून को जो हुकूमत चलाने की पूरी-पूरी योग्यता रखता था, कामयाबी मिली। इस प्रकार अब्बासी सल्तनत एक बार फिर संगठित हो गई। यदि मामून फिर से सल्तनत संगठित करने में कामयाब न होता तो अब्बासियों का पतन पचास साल पहले ही शुरू हो जाता।
मामून रशीद (198 हि०/818 ई० से 218 हि०/833 ई०)
हारून रशीद के बाद यदि किसी और अब्बासी ख़लीफ़ा का दौर हारून के दौर का मुक़ाबला कर सकता है, तो वह मामून रशीद का शासनकाल है।
अमीन के क़त्ल होने के बाद भी मामून रशीद तक़रीबन 6 साल तक मरू ही में रहा। उस ज़माने में इराक़, विशेषकर बग़दाद हंगामों की भेंट चढ़ गया। इन हंगामों की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मामून रशीद अपने शिया-गुरु और प्रशिक्षकों की वजह से हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की श्रेष्ठता का क़ायल हो गया था और वह हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद को ख़िलाफ़त का ज़्यादा हक़दार समझता था। इस मामले में वह यहाँ तक बढ़ गया कि उसने इमाम अली बिन मूसा रज़ा को जो शिया के आठवें इमाम हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस फ़ैसले ने अब्बासी शहज़ादों में बेचैनी पैदा कर दी और उन्होंने इराक़ में बग़ावत कर दी। मामून रशीद को आख़िरकार अपना फ़ैसला रद्द करना पड़ा और मरू छोड़कर बग़दाद आना पड़ा। 204 हि०/819 ई० में बग़दाद आने के बाद हंगामे ख़त्म हो गए और मामून की ख़िलाफ़त के बाक़ी चौदह साल शान्तिपूर्ण गुज़रे।
मामून के ज़माने में तबरिस्तान का इलाक़ा भी हंगामों की लपेट में रहा। यहाँ एक ईरानी 'बाबक ख़रमी' ने पहाड़ी इलाक़ों पर क़बज़ा जमा लिया। उसने एक नए मज़हब की बुनियाद डाली थी। वह एक आन्दोलन का अलमबरदार था जो प्रत्यक्षतः मज़हबी रंग में रंगा था लेकिन हक़ीक़त में यह आन्दोलन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक राजनीतिक आन्दोलन था और उसका उद्देश्य ईरानियों की हुकूमत क़ायम करना था। मामून की कोशिश के बावजूद उस बग़ावत पर क़ाबू नहीं पाया जा सका।
मामून के दौर की एक अहम घटना 'सक़लिया' और 'क्रेट' (Crete) द्वीपों की फ़तह है। सक़लिया क़ैरवान के अग़लिबी हुक्मरानों की कोशिशों से फ़तह हुआ और क्रेट द्वीप अंदलुस (स्पेन) से निकली हुई मुसलमानों की एक जमाअत ने फ़तह किया।
मामून रशीद के दौर की एक और विशेषता यह है कि उसके ज़माने में तुर्कों में इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। अशरोसना और काबुल के हुक्मरानों ने इसी ज़माने में इस्लाम क़बूल किया।
मामून रशीद स्वभाव और आचरण में अपने बाप जैसा था, बल्कि वह हारून रशीद के मुक़ाबले में ज़्यादा नर्म दिल था। वह दानशील भी हारून से ज़्यादा था और ज्ञान एवं साहित्य की उसने जिस प्रकार सरपरस्ती की उसकी मिसाल शायद इतिहास में नहीं मिल सकती।
मामून रशीद को न्याय (इनसाफ़) का बड़ा ख़याल रहता था। वह हर रविवार को सुबह से ज़ुह्र तक ख़ुद प्रजा की शिकायतें सुनता था। उसकी अदालत में एक मामूली आदमी शहज़ादों तक से अपना हक़ ले सकता था।
एक बार एक ग़रीब बूढ़ी औरत ने दावा किया कि मामून के लड़के अब्बास ने उसकी जायदाद पर क़बज़ा कर लिया है। जब मुक़द्दमा पेश हुआ तो मामून ने अब्बास को बुढ़िया के पास खड़ा करके दोनों के बयान लिए। शहज़ादा बाप के आदर के कारण धीरे-धीरे बोलता था और बुढ़िया की आवाज़ बुलन्द थी। प्रधानमन्त्री अहमद बिन अबी ख़ालिद ने इसपर बुढ़िया को रोका कि अमीरुल मोमिनीन के सामने ऊँची आवाज़ में बोलना अदब के ख़िलाफ़ है, परन्तु मामून ने उसे रोका और कहा कि वह जिस तरह कहती है कहने दो। हक़ ने उसकी आवाज़ बुलन्द कर दी है और अब्बास को गूँगा कर दिया है। दोनों के बयान सुनने के बाद मामून ने बुढ़िया के हक़ में फ़ैसला किया और उसकी जायदाद वापस कर दी।
मामून की न्यायप्रियता की और भी बहुत-सी घटनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उसपर बीस हज़ार का दावा किया। मामून को क़ाज़ी की अदालत में हाज़िर होना पड़ा। नौकरों ने उसके लिए अदालत में क़ालीन बिछा दिया। चीफ़ जस्टिस (क़ाज़ी-उल-क़ुज़ात) ने यह देखा तो नौकरों को रोक दिया और कहा कि अदालत में दावा करनेवाला और अपराधी दोनों बराबर हैं। किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। मामून ने जब क़ाज़ी का ऐसा इनसाफ़ देखा तो उसकी तनख़्वाह बढ़ा दी। अब हर आदमी अंदाज़ा कर सकता है कि जिस ज़माने में ऐसे हिम्मतवाले क़ाज़ी (जज) हों और ऐसे इनसाफ़पसंद बादशाह हों तो आम लोग कैसे चैन और अमन की ज़िन्दगी गुज़ारते रहे होंगे।
मामून के स्वभाव में हद से ज़्यादा सादगी और नम्रता थी, घमण्ड लेशमात्र भी न था। अपने साथियों और दरबारियों में बड़ी सादगी और सहजता से रहता था। उसके दौर के प्रसिद्ध चीफ़ जस्टिस यहया बिन अकसम का बयान है कि एक रात मुझे मामून के पास सोने का संयोग हुआ। आधी रात गए मुझे प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठा। मामून की नज़र पड़ गई। पूछा "क़ाज़ी साहब क्या बात है?"
“अमीरुल मोमिनीन! प्यास लगी है।" क़ाज़ी ने जवाब दिया।
मामून यह सुनकर उठा और ख़ुद जाकर पानी ले आया। इसपर क़ाज़ी साहब ने कहा—
“अमीरुल मोमिनीन! नौकरों को क्यों नहीं आवाज़ दी।"
“सब सो रहे हैं।” मामून ने कहा।
"तो मैं ख़ुद जाकर पानी पी लेता।" क़ाज़ी साहब ने कहा।
“यह बुरी बात है कि अपने मेहमान से काम लिया जाए। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है कि क़ौम का सरदार उनका ख़ादिम (सेवक) है।" मामून ने जवाब दिया।
मामून रशीद को प्रशासन-व्यवस्था का इतना ख़याल था कि वह अपनी विस्तृत सल्तनत की हर चीज़ और हर काम से वाक़िफ़ रहना चाहता था। उसने इस मक़सद के लिए सारे मुल्क में जासूस नियुक्त कर रखे थे, जो ज़रा ज़रा-सी बात की ख़लीफ़ा को सूचना देते थे। सिर्फ़ बग़दाद में इस काम के लिए सतरह सौ औरतें नियुक्त थीं जो उसे गुप्त सूचनाएँ पहुँचाती रहती थीं।
ज्ञान एवं कला के विकास के लिए मामून रशीद की कोशिशें इतिहास के सुनहरे अध्याय हैं। वह ख़ुद भी एक बड़ा आलिम था। ख़लीफ़ाओं में उसके बराबर कोई दूसरा आलिम नहीं हुआ। वह हाफ़िज़े क़ुरआन था और धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होने के अलावा उसे खगोल-शास्त्र और गणित से बड़ी दिलचस्पी थी। उसने गणितज्ञों एवं खगोल शास्त्रियों की मदद से दो बार भूमण्डल को नपवाया।
दूसरी भाषा से अनुवाद का काम मामून रशीद के काल में चरम पर पहुँच गया। वह अनुवाद करनेवालों को अनुवाद की हुई किताबों के वज़न के बराबर चाँदी या सोना इनाम में दिया करता था। दर्शन-शास्त्र एवं बौद्धिक-शास्त्र के अनुवाद के सिलसिले में इतिहासकारों ने एक दिलचस्प वाक़िआ लिखा है। वे लिखते हैं :-
"यह वह ज़माना था कि बौद्धिक ज्ञान रूमा में एक मुसीबत समझे जाते थे। इनसे सम्बन्धित किताबें क़ुस्तनतीनिया के एक मकान में बंद कर दी गई थीं और हर बादशाह इस मकान में एक ताला और जड़ देता था। मामून रशीद ने जब इन किताबों को बग़दाद भेजने की इच्छा प्रकट की तो क़ैसर ने अपने सलाहकारों से पूछा कि यदि ये किताबें बग़दाद भेज दी जाएँ तो मुझपर दुनिया में कोई मुसीबत और परलोक में कोई पूछ-ताछ तो न होगी। उसपर एक धर्म गुरु ने जवाब दिया, मुसीबत और पूछ-ताछ नहीं बल्कि सवाब मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जिस मंसब में दाख़िल हो जाएँ उसकी बुनियादें हिला दें। अत: ये किताबें जो अफ़लातून (Platou), सुक़रात (Socrates), अरस्तु (Aristotle), जालीनूस (Galen), अक़्लीदस (Eukleides) और बतलीमूस (Ptolemy) आदि की लिखी हुई थीं, बग़दाद भेज दी गईं।"
मामून रशीद के दौर की एक अहम घटना 'फ़ितन-ए-ख़ल्क़े क़ुरआन' है। दर्शन-शास्त्र के अध्ययन और ग़ैर मुस्लिम विद्वानों की संगति के कारण मामून रशीद इस अक़ीदे का क़ायल हो गया कि क़ुरआन मख़लूक़ (रचना) है। इस नज़रिया की सच्चाई पर मामून को इस हद तक यक़ीन था कि उसने ख़ल्क़े क़ुरआन के नज़रिया को इस्लाम और क़ुफ़्र का पैमाना समझ लिया था। उसने आलिमों को मजबूर किया कि या तो इस नज़रिया को स्वीकार करें या फिर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ।
अब तक यदि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कुछ पाबन्दी थी तो सिर्फ़ सियासी मामलात में थी परन्तु मामून जैसे समझदार और विद्वान हुक्मरान ने 'ख़ल्क़े क़ुरआन' के मसले में कट्टरता अपनाकर मज़हबी आज़ादी में भी हस्तक्षेप कर दिया। मामून रशीद का तो जल्द ही इंतिक़ाल हो गया, परन्तु उसके दो उत्तराधिकारियों 'मोतसिम' और 'वासिक़' के ज़माने में इस मसले के कारण आलिमों पर और विशेषकर इमाम अहमद बिन हंबल (रहमतुल्लाह अलैह) पर बहुत सख़्तियाँ की गईं। हालाँकि उनका कहना सिर्फ़ यह था कि किताब (क़ुरआन) एवं सुन्नत (हदीस) के मुताबिक़ किसी शख़्स को उस क़िस्म के अक़ीदे पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
मामून रशीद का 48 साल की उम्र में इंतिक़ाल हुआ। उसने बीस साल हुकूमत की।
मोतसिम (218 हि०/833 ई० से 227 हि०/842 ई०)
मामून के बाद उसका भाई मोतसिम बिल्लाह तख़्त पर बैठा। मोतसिम के ज़माने में फ़ौजी ताक़त में बड़ी वृद्धि हुई और उसने इस मक़सद के लिए तुर्कों की फ़ौज तैयार की। मोतसिम के दौर की सबसे प्रसिद्ध घटना रूम पर हमला है। क़िस्सा यह है कि मोतसिम दरबार में बैठा हुआ था कि उसे मालूम हुआ कि रूमियों ने सरहद पर हमला करके बहुत-से मुसलमानों को क़ैद कर लिया है। उन क़ैदियों में एक बूढ़ी औरत भी थी, जो गिरफ़्तार होने पर उसका नाम लेकर मदद को पुकार रही थी। मोतसिम ने यह सुना तो उससे सब्र न हो सका। तुरन्त लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया। इस मौक़े पर एक ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर बताया कि यह समय अशुभ है, अत: लश्कर की रवानगी रोक दीजिए। परन्तु मोतसिम नहीं माना और हमला कर दिया। उसकी फ़ौजों ने एशिया-ए-कोचक को रौंद डाला और उस वक़्त तक वापस नहीं लौटा जब तक उस बुढ़िया को मुक्त न करा लिया।

चित्र 3 :- क़ाहिरा की यह मसजिद 876 ई०/263 हि० और 879 ई०/265 हि० के बीच तामीर हुई लेकिन इसका मीनार 1296 ई०/696 हि० की तामीर है। यह मस्जिद मिस्र और इस्लामी दुनिया में मुसलमानों के इब्तिदाई फ़न्ने-तामीर की एक अहम यादगार है।
मोतसिम इस मुहिम के दौरान अमूरिया और अनक़रह की क़िलाबंदियों को ढाता हुआ क़ुस्तनतीनिया के क़रीब तक पहुँच गया था और रूम की राजधानी को फ़तह करने की तैयारियाँ कर रहा था कि उसे अपने भतीजे अब्बास की बग़ावत की सूचना मिली, जिसके कारण यह मुहिम अपूर्ण छोड़कर मोतसिम को बग़दाद वापस आना पड़ा। जब मोतसिम इस कामयाब मुहिम से वापस लौटा तो मशहूर शायर अबू तमाम ने मोतसिम की शान में एक क़सीदा पढ़ा और कहा कि तक़दीर के फ़ैसले सितारे नहीं करते, तलवार करती है।
मोतसिम के दौर की एक दूसरी अहम घटना 'बाबक ख़रमी' की बग़ावत का ख़ात्मा है। बाबक ख़रमी एक गैर मुस्लिम ईरानी था और उसने एक ऐसा आन्दोलन शुरू किया था जिसका मक़सद मुसलमानों को गुमराह और दीन से दूर करना था। इस इस्लाम-दुश्मन आन्दोलन के द्वारा उसने बहुत-से ईरानियों को अपने साथ मिला लिया था और गीलान और आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाक़ों पर क़बज़ा कर लिया था। बाबक ख़रमी की यह बग़ावत मामून रशीद के ज़माने ही में शुरू हो गई थी। इसे आख़िरकार मोतसिम ने कुचला। बाबक गिरफ़्तार कर लिया गया और क़त्ल कर दिया गया।
मोतसिम ने बग़दाद से उत्तर में तक़रीबन 75 मील दूर दजला नदी के किनारे 'सामरा' के नाम से एक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस शहर ने बड़ी तरक़्क़ी की और अपनी शानदार इमारतों और ख़ूबसूरती में बग़दाद का मुक़ाबला करने लगा। सामरा 221 हि०/836 ई० से 279 हि०/892 ई० तक राजधानी रही, उसके बाद बग़दाद पुनः राजधानी बन गई।
मुतवक्किल (232 हि०/847 ई० से 247 हि०/861 ई०)
मोतसिम के बाद उसका लड़का वासिक़ और उसके बाद वासिक़ का भाई मुतवक्किल ख़िलाफ़त के तख़्त पर बैठा। मुतवक्किल का दौर अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान का आख़िरी दौर है। उसके दौर में ख़ुशहाली आम थी और चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थीं। मुतवक्किल नर्म स्वभाव का था। वह कहा करता था कि मुझसे पहले के ख़लीफ़ा प्रजा पर इसलिए सख़्ती करते थे कि वे उस सख़्ती के कारण उनके आज्ञाकारी रहें लेकिन मैं नर्मी करता हूँ, ताकि प्रजा मुझसे प्रेम करे। मुतवक्किल ने ख़ल्क़े क़ुरआन के मसले की सरपरस्ती ख़त्म कर दी और इस क़िस्म के मसलों पर वाद-विवाद और बहस-मुबाहिसे बंद करा दिए।
चित्र  4 :- मसजिद सामरा का मीनार
4 :- मसजिद सामरा का मीनार
यह मीनार अब्बासी ख़लीफ़ा मुतवक्किल बिल्लाह (232 हि०/847 ई० से 247 हि०/861 ई०) ने नये दारुल ख़िलाफ़ा सामरा में बनवाया था—यह मीनार जिसकी बुलन्दी 175 फुट है अपने अनोखे तर्ज़े तामीर की वजह से एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है।
मुतवक्किल बहरहाल एक बादशाह था, किसी प्रजातांत्रिक हुकूमत का संचालक नहीं था। बादशाह के अन्दर जो डिक्टेटरशिप और अपनी बात मनवाने की भावना होती है, वह मुतवक्किल में भी थी। और उसके द्वारा इसकी अभिव्यक्ति बड़े भोंडे अंदाज़ से हुई। मुतवक्किल हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद की ओर से हमेशा बग़ावत का ख़तरा महसूस करता रहता था। इसी तरह रूमियों से लगातार सरहदी लड़ाइयों के कारण सल्तनत की ईसाई आबादी को भी शक की निगाह से देखता था। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद के सम्बन्ध में उसने अपने जज़्बात की अभिव्यक्ति इस प्रकार की कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) का मज़ार ढाया और ईसाइयों से सम्बन्धित उसने अपने जज़्बे की अभिव्यक्ति उनपर कुछ पाबंदियाँ लगाकर की। उनमें एक पाबन्दी यह थी कि वे एक विशेष लिबास पहना करें।
बनू अब्बास का पतन
मुतवक्किल अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान काल का अन्तिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद अब्बासी ख़िलाफ़त का पतन शुरू हो गया और अब्बासियों की विस्तृत सल्तनत की सीमाएँ कम होती चली गईं।
बनू अब्बास का पतन इस कारण नहीं हुआ कि उनके हुक्मरान अयोग्य थे। अब्बासियों के पतनकाल में भी कई ऐसे हुक्मरान नज़र आते हैं जो बुद्धिमान और योग्य थे। अब्वासियों के पतन का सबसे बड़ा कारण तुर्कों की सत्ता थी, जो मोतसिम के ज़माने से बढ़नी शुरू हो गई थी। अब्बासी हुकूमत की स्थापना में चूँकि ईरानियों का बहुत बड़ा हाथ था इसलिए हुकूमत पर उनका प्रभाव प्रारंभ से ही था। वज़ीर और दूसरे उच्च अधिकारी आम तौर पर ईरानी होते थे। मामून रशीद के बाद ईरानी प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ख़िलाफ़त की मज़बूती के लिए यह बात बड़ी अच्छी थी कि अरब और ईरानी एक-दूसरे से लड़ने के बदले अब ख़िलाफ़त की मज़बूती में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। इस सहयोग को भाईचारे और समानता की इस्लामी बुनियाद पर और बढ़ाया जा सकता था, परन्तु दरबार से इस्लामी रूह और इस्लामी दृष्टिकोण को उसी समय विदा किया जा चुका था जब ख़िलाफ़त की जगह मुलूकियत (बादशाहत) क़ायम हुई थी। अब सियासत की बुनियाद इस्लामी मिल्लत के कल्याण के बजाए हुक्मरान के व्यक्तिगत स्वार्थों पर होती थी। अब्बासियों ने प्रारंभिक दौर में उन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों के तहत ईरानियों को आगे बढ़ाया और अब मोतसिम ने उन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों के तहत ईरानियों की बढ़ती हुई शक्ति से डरकर तुर्कों को आगे बढ़ाया।
अब्बासी ख़िलाफ़त के ज़माने में तुर्कों ने बड़ी तेज़ी से इस्लाम क़बूल करना शुरू कर दिया था। मोतसिम ने अपने निजी सुरक्षा-गार्ड के तौर पर और फ़ौज के लिए पूर्वी सीमाओं से हज़ारों की संख्या में तुर्कों को भरती किया। तुर्क चूँकि स्वभावतः जंगजू और साहसी होते थे इसलिए वे जल्द ही फ़ौजी-तन्त्र में छा गए। मुतवक्किल के ज़माने में उनका ज़ोर इतना बढ़ गया कि वे सल्तनत के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे और आख़िरकार स्वयं मुतवक्किल उनके षड्यन्त्र का शिकार होकर क़त्ल हुआ। तुर्क फ़ौजी और उनके अफ़सरों में सब मुसलमान नहीं थे। उनकी एक बड़ी संख्या अब तक ग़ैर मुस्लिम थी। वे अप्रशिक्षित और गँवार थे। उनके इसी गँवारपन के कारण मोतसिम को बग़दाद छोड़कर 'सामरा' जाना पड़ा। उनमें जो मुसलमान थे उन्हें सही तरीक़े से इस्लामी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं मिल पाया था और वे उतने पक्के मुसलमान भी नहीं थे जितने ईरानी थे। यही कारण है कि अरब हुक्मरानों और ईरानी अमीरों और वज़ीरों की तरह ये तुर्क भी हर बात इस्लामी मिल्लत के कल्याण के बजाए अपने हित में सोचने लगे और इस प्रकार इस्लामी ख़िलाफ़त के अरब, ईरानी और तुर्क बाशिन्दे इस्लाम के मूल लक्ष्य को नज़रअंदाज़ कर देने के कारण जातीय और क्षेत्रीय आधार पर एक-दूसरे से टकराने लगे।
मुतवक्किल के बाद तुर्कों की शक्ति और बढ़ गई। अब वे ख़लीफ़ा का आदेश सुनने से भी इनकार करने लगे। उन्होंने कई ख़लीफ़ाओं को तख़्त से उतार दिया और कई को क़त्ल भी किया। मुतवक्किल के बाद आठ साल के अल्पावधि में चार ख़लीफ़ा तख़्त पर बिठाए और उतारे गए। इस प्रकार तुर्कों ने केन्द्रीय हुकूमत को कमज़ोर तो कर दिया परन्तु ख़ुद कोई मज़बूत हुकूमत क़ायम न कर सके। जब सल्तनत के विभिन्न विभागों ने यह हालत देखी तो वहाँ के गवर्नरों और सूबेदारों ने अपने-अपने इलाक़े में आज़ाद हुकूमतें क़ायम कर लीं। [उन आज़ाद हुकूमतों के नाम ये हैं :
(i) सफ़्फ़ारिया (253 हि०/867 ई० से 298 हि०/910 ई०) - इस हुकूमत का संस्थापक याक़ूब बिन लैस सफ़्फ़ार था। सम्पूर्ण दक्षिणी ईरान इसके क़बज़े में था। इस हुकूमत का ख़ात्मा 'सामानियों' के हाथ हुआ।
(ii) दौलते अलविया, तबरिस्तान (257 हि०/870 से 316 हि०/928 ई०) - इसके संस्थापक हसन बिन ज़ैद अलवी थे और यह ईरान के उत्तरी भाग 'माज़न्दरान' में क़ायम हुई थी जिसे उस ज़माने में तबरिस्तान कहते थे। इस हुकूमत का ख़ात्मा भी 'सामानियों' ने किया।
(iii) दौलते तूलूनिया, मिस्र (254 हि०/868 ई० से 292 हि०/904 ई०) - इस हुकूमत का संस्थापक एक तुर्क अहमद बिन तूलून (254 हि० से 270 हि०) था। मिस्र और शाम (सीरिया) इसके क़बज़े में थे। यह हुकूमत मज़बूत और प्रजा का ख़याल रखनेवाली थी। क़ाहिरा की मशहूर मसजिद जामे इब्ने तूलून इसी दौर में बनी।
(iv) दौलते सामानिया (261 हि०/874 ई० से 395 हि०/1004 ई०) - इस हुकूमत का हाल अगले अध्याय में आएगा। यह ईरानी हुकूमत थी।
(v) आले हमदान (293 हि०/905 ई० से 406 हि०/1015 ई०) - यह अरबों की हुकूमत थी। पहले इसका केन्द्र मोसिल में था, फिर हलब (सीरिया) हो गया। हमदानी हुक्मरानों में सैफ़ुद्दौला (333 हि०/944 से 356 हि०/967 ई०) का नाम उल्लेखनीय है।
मुसलमानों में गृह युद्ध शुरू हो जाने के कारण रूमी ज़ोर पकड़ गए थे। सैफ़ुद्दौला की हुकूमत हालांकि छोटी-सी थी लेकिन उसने एशिया-ए-कोचक में रूमियों के आक्रमण को कामयाबी से रोका। इसके अतिरिक्त सैफ़ुद्दौला ज्ञान एवं साहित्य का बहुत बड़ा सरपरस्त था। अरबी का सबसे बड़ा शायर मुतनब्बी (915 ई० से 965 ई०) और मशहूर दार्शनिक फ़ाराबी उसके दरबार से वाबस्ता थे।
(vi) दौलते ज़ियारिया या आले दश्मगीर (319 हि०/931 ई० से 430 हि०/1038 ई०) - यह ईरानी हुकूमत थी और ईरान के उत्तरी-पूर्वी सूबा जुरजान या गुरगान में क़ायम हुई।
(vii) दौलते-अख़शीदिया (323 हि०/935 से 357 हि०/968 ई०) - यह तुर्कों की हुकूमत थी। तूलूनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मिस्र और शाम पर फिर अब्बासी ख़लीफ़ा की सत्ता क़ायम हो गई थी, परन्तु चंद सालों के बाद यह इलाक़े फिर उनके हाथ से निकल गए और यहाँ अख़शीदी हुकूमत क़ायम हो गई। जिसका ख़ात्मा उत्तरी अफ़्रीक़ा की फ़ातिमी हुकूमत ने किया। अख़शीदियों का वज़ीर एक हब्शी मलिक काफ़ूर था जो बड़ा क़ाबिल और ज्ञान-विज्ञान का चाहनेवाला था।
यह हुकूमतें ज़्यादा मज़बूत और बड़ी नहीं थीं। बड़ी और मज़बूत हुकूमतें सामानियों, बनी बुविया और बनी फ़ातिमा की थी जिनका हाल हम अलगे अध्याय में पढ़ेंगे।] ये हुकूमतें अब्बासी ख़िलाफ़त को स्वीकार करती थीं, उनकी मसजिदों में अब्बासी ख़लीफ़ा के नाम का ख़ुत्बा पढ़ा जाता था, लेकिन अब्बासी ख़लीफ़ा का कोई हुक्म नहीं चलता था।
पतन के इस दौर में जो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं उनमें दो उल्लेखनीय हैं। इनमें एक घटना हबशियों की बग़ावत है। अरबों के पास जो ग़ुलाम थे वे अधिकतर हबशी थे। एक ईरानी ने उन हबशी ग़ुलामों की मदद से इराक़ में हंगामा शुरू कर दिया। हबशियों की तादाद मुल्क में काफ़ी थी। वे सब उसके साथ मिल गए। इन हबशियों ने दक्षिणी इराक़ और ख़ूज़िस्तान पर क़बज़ा कर लिया और मुसलमानों पर ज़ुल्म किए। कहा जाता है कि उनके हाथ से पचीस लाख बेगुनाह नागरिक मारे गए। यह बग़ावत 255 हि०/869 ई० से 270 हि०/883 ई० तक यानी पन्द्रह साल तक जारी रही।
इस दौर की दूसरी अहम घटना क़रामिता का फ़ित्ना है। बसरा के क़रीब रहनेवाले एक शख़्स क़रमत ने मुल्क की अशान्ति से फ़ायदा उठाकर एक नए मज़हब की बुनियाद डाल दी, जिसके अनुयायी क़रामती या क़रामिता कहलाते हैं। क़रामिता के फ़ित्ने का प्रारंभ 278 हि०/891 ई० में हुआ और पचास साल से ज़्यादा जारी रहा। उत्तरी इराक़ और शाम (सीरिया) उनके ज़ुल्मो सितम और लूटमार का सबसे ज़्यादा निशाना बने। ये लोग यहाँ तक बढ़ गए थे कि 317 हि०/929 ई० में हज के मौक़ा पर हाजियों का क़त्ले आम किया और हज्रे असवद उठाकर अपनी राजधानी हिज्र ले गए, जो बसरा के दक्षिण में स्थित था। बाद में फ़ातिमी हुक्मरान उबैदुल्लाह के हुक्म पर हज्रे असवद वापस कर दिया।
पतनकाल के अब्बासी हुक्मरानों में कुछ बहुत अच्छे और योग्य थे और उन्होंने पतन को रोकने की काफ़ी कोशिश की। उन हुक्मरानों में एक 'मुहतदी' है। उसने अब्बासी ख़िलाफ़त को अधिक से अधिक इस्लामी रंग देने की कोशिश की। वह कहता था कि मुझे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के रास्ते पर चलने दो ताकि मैं भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) जैसी मिसाल पैदा कर सकूँ। परन्तु गँवार तुर्की, शाही हाकिमों और मंत्रियों ने, जो इस्लामी पाबंदियों से घबराते थे, मुहतदी को कामयाब नहीं होने दिया और यह ख़लीफ़ा तुर्कों के हाथों क़त्ल हो गया।
कहा जाता है कि मुहतदी को गिरफ़्तार करने के बाद तुर्कों ने उससे सवाल किया कि तुम लोगों को ऐसे रास्ते पर क्यों चलाना चाहते हो जिससे वे अनभिज्ञ हैं। मुहतदी ने जवाब दिया कि मैं लोगों को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े पर चलाना चाहता हूँ। इसपर तुर्कों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सम्पर्क ऐसे लोगों से था जो दुनिया से कटकर आख़िरत की ओर उन्मुख रहते थे और तुम्हारे साथी तुर्क, ख़ज़र आदि ऐसी क़ौमें हैं जो आख़िरत के फ़र्ज़ों से अनभिज्ञ हैं और उनकी ज़िन्दगी का मक़सद दुनियावी लाभ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऐसी हालत में तुम उन्हें कैसे रास्ते पर चला सकते हो?
तुर्कों का यह जवाब इस बात का सबूत है कि तीसरी सदी हिजरी के मध्य तक दरबार का माहौल किस हद तक ग़ैर इस्लामी हो चुका था।
ख़लीफ़ा मोतमिद का भाई मोफ़िक़ (मृत्यु 278 हि०/891 ई०) भी उस दौर का प्रमुख व्यक्ति है। वह हालाँकि ख़लीफ़ा नहीं था, लेकिन हुकूमत की बागडोर उसी के हाथ में थी। वह एक अच्छा सिपहसालार था। उसने ख़िलाफ़त की साख क़ायम रखने की पूरी कोशिश की, हबशियों की बग़ावत उसी ने ख़त्म की और तुर्कों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया।
मोतज़िद (279 हि०/892 ई० से 289 हि०/902 ई०)
पतनकाल में जिस ख़लीफ़ा ने सबसे ज़्यादा काम किए वह मोफ़िक़ का बेटा मोतज़िद है जो मोतमिद के बाद तख़्ते ख़िलाफ़त पर बैठा। मोतज़िद ने तुर्कों का ज़ोर तोड़ा और एक विस्तृत इलाक़े में जिसमें अरब, इराक़, पश्चिमी ईरान और आरमीनिया के क्षेत्र आते थे, फिर से शान्ति व्यवस्था क़ायम कर दी और अब्बासी हुकूमत की गिरती हुई इमारत को सहारा दिया। उसके दौर में मिस्र एवं शाम (सीरिया) की तूलूनी हुकूमत ने भी अब्बासी ख़िलाफ़त की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके उत्तराधिकारी मुकतफ़ी के ज़माने में मिस्र एवं शाम (सीरिया) सीधे अब्बासी ख़िलाफ़त के क़बज़े में आ गए। अपने कारनामे के कारण मोतज़िद को अब्बासी ख़िलाफ़त का दूसरा संस्थापक कहा जाता है।
मोतज़िद ने शान्ति-व्यवस्था क़ायम करने के सिलसिले में काफ़ी कठोरता से काम लिया, परन्तु उसके साथ ही साथ उसने मुसलमानों की नैतिक एवं वैचारिक सुधार की भी कोशिश की। वह निजी तौर पर दीनदार इनसान था। उसने ज्योतिषों को सड़कों पर बैठने से मना कर दिया। दर्शन-शास्त्र की उन किताबों पर, जो मुसलमानों में गुमराही फैला रही थीं, पाबंदी लगा दी। ईरानी आतिशपरस्तों से प्रभावित होकर कुछ मुसलमानों में भी ग़लत रस्म-रिवाज पैदा हो गए थे, मोतज़िद ने इस रस्म को आदेश देकर बन्द कर दिया। मोतज़िद के ज़माने में अदालतें भी आज़ाद हो गई थीं और उच्च पदाधिकारी ही नहीं ख़लीफ़ा भी अदालत से बच नहीं सकता था।
मोतज़िद के ज़माने में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पुराने टैक्स भी कम कर दिए गए, परन्तु इसके बावजूद अब्बासी हुकूमत का बजट इतना अच्छा हो गया था कि ख़र्च के बाद एक बड़ी रक़म बच जाती थी।
मोतज़िद के बाद एक के बाद एक उसके तीन लड़के मुक्तफ़ी बिल्लाह, मुक़्तदिर बिल्लाह और क़ाहिर बिल्लाह के नाम से तख़्त पर बैठे। मुक्तफ़ी अच्छा हुक्मरान था, लेकिन उसके बाद हालात फिर बदल गए। उसके उत्तराधिकारी मुक़्तदिर बिल्लाह ने पचीस साल हुकूमत की, परन्तु सारा ज़माना हंगामों एवं आतंकों की भेंट चढ़ गया। यह हुक्मरान सुविधाभोगी, ऐशपरस्त और शराब एवं कबाब का रसिया था। अतः दरबार नाचने और गानेवालियों का केन्द्र बन गया। उसने दरबार का ख़र्च बहुत बढ़ा लिया था। शाही महल में ग्यारह हज़ार ख़्वाजासरा थे। मोतज़िद और मुक्तफ़ी के ज़माने में सरकारी ख़ज़ाना भरा रहता था। परन्तु अब यह हाल हो गया कि फ़ौज की कई-कई माह की तनख़्वाह चढ़ जाती थी। नतीजा यह हुआ कि पुनः बग़ावत हुई और मुक़्तदिर बिल्लाह को अपदस्थ करके क़त्ल कर दिया गया।
मुक़्तदिर बिल्लाह के दौर की एक विशेष घटना बुलग़ार में इस्लाम का प्रसार है। बुलग़ार रूस में वाल्गा नदी के किनारे उस जगह जहाँ अब शहर काज़ान' आबाद है, तुर्कों का एक शहर था। यहाँ के हुक्मरान ने इस्लाम क़बूल करने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल बग़दाद भेजा ताकि वह बुलग़ार के इलाक़े में इस्लाम के प्रसार और मुसलमानों को शिक्षा देने के मामले में ख़लीफ़ा से मदद माँगे। मुक़्तदिर बिल्लाह ने उनकी माँग स्वीकार करते हुए इब्ने फ़ुज़लान के नेतृत्व में एक जमाअत बुलग़ार भेजी। [बुलग़ार वाल्गा नदी की वादी में मुसलमानों की पहली सल्तनत थी जो तक़रीबन दो सौ साल तक क़ायम रही।]
मुक़्तदिर बिल्लाह के उत्तराधिकारी क़ाहिर बिल्लाह के दौर में मुक़्तदिर के दौर की अय्याशी के ख़िलाफ़ तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाचने-गानेवाली औरतों के पेशे और शराब पर पाबन्दी लगा दी गई। गानेवालों को क़ैद और हिजड़ों को देश-निकाला दे दिया गया। परन्तु यह एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। इसके पीछे न कोई विचार था न कोई संस्था थी। क़ाहिर बिल्लाह उपरोक्त सुधारों के बाद भी स्वयं शराब न छोड़ सका और न हसीन लौंडियों की संगति तर्क की।
मुसलमानों की गिरती हुई नैतिक हालत के ख़िलाफ़ इसी प्रकार की एक प्रतिक्रिया बग़दाद में क़ाहिर के उत्तराधिकारी राज़ी बिल्लाह के दौर में अवामी सतह पर भी हुई। इमाम अहमद बिन हंबल के अनुयायियों ने जो 'हंबली' कहलाते थे, अवामी सतह पर समालोचना शुरू कर दी। वह फ़ौजी अफ़सरों और आम लोगों के घरों पर छापे मारते। जहाँ नबीज़ (एक प्रकार की शराब) नज़र आती, उसे बहा देते। गानेवाली औरतों को मारते, वाद्ययन्त्र तोड़ डालते, मर्दों को औरतों के साथ चलने से रोकते। लेकिन यह आन्दोलन असंगठित और भवनात्मक था। इसके पीछे न कोई ठोस विचार था और न ही कोई संगठित पार्टी। नतीजा यह हुआ कि हंबलियों का यह आंदोलन हंबलियों और शाफ़ियों (इमाम शाफ़ई के अनुयायी) के झगड़े में बदल गया।
मुख़्तसर यह कि हुक्मरानों की ऐशपरस्ती, अयोग्यता, गवर्नरों की स्वेच्छाचारिता और नैतिक पतन के नतीजे में ख़िलाफ़त की सीमाएँ फिर घटना शुरू हो गईं। राज़ी बिल्लाह का उत्तराधिकारी मुत्तक़ी बिल्लाह हालाँकि अपने नाम की तरह ही नेक था, लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें और कोई ख़ूबी नहीं थी। शासन व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। आख़िरकार पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में क़ायम होनेवाली हुकूमत बनी बुवया के एक हुक्मरान मुअज़्ज़द्दौला ने 334 हि०/945 ई० में बग़दाद पर क़बज़ा कर लिया। ख़िलाफ़त अब भी क़ायम रही क्योंकि मुसलमान ख़िलाफ़त को इस्लामी राजनीतिक-व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा समझते थे। और एक ख़लीफ़ा के बाद दूसरा खलीफ़ा तख़्त पर बैठता रहा, परन्तु उन ख़लीफ़ाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था, हुकूमत दूसरों की थी।
यह हालत दो सौ साल तक रही। उसके बाद ख़लीफ़ा फिर आज़ाद हो गए, परन्तु उनकी हुकूमत इराक़ तक सीमित रही। वह कोई बड़ी सल्तनत क़ायम न कर सके और जैसाकि हम आगे चलकर बयान करेंगे, अब्बासी ख़लीफ़ा की यह आज़ाद हुकूमत सौ-सवा सौ साल क़ायम रहने के बाद तातारियों के हाथों ख़त्म हो गई।
अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान का ज़माना 132 हि०/750 ई० से 247 हि०/861 ई० तक है। उसके बाद पतन शुरू हो गया और 334 हि०/945 ई० में बनी बुवया के हाथों अब्बासी ख़लीफ़ा की सम्प्रभुता ख़त्म हो गई।
अब्बासी ख़िलाफ़त
132 हि०/750 ई० से 656 हि०/1258 ई०
उत्थानकाल
1. अबुल-अब्बास सफ़्फ़ाह - 132 हि०/750 ई० से 136 हि०/754 ई०
2. अबू जाफ़र मंसूर - 136 हि०/754 ई० से 158 हि०/775 ई०
3. मुहम्मद महदी - 158 हि०/775 ई० से 169 हि०/785 ई०
4. मूसा हादी - 169 हि०/785 ई० से 170 हि०/786 ई०
5. हारून रशीद - 170 हि०/786 ई० से 193 हि०/809 ई०
6. अमीन रशीद - 193 हि०/809 ई० से 198 हि०/813 ई०
7. मामून रशीद - 198 हि०/813 ई० से 218 हि०/833 ई०
8. मोतसिम बिल्लाह - 218 हि०/833 ई० से 227 हि०/842 ई०
9. वासिक़ बिल्लाह - 227 हि०/842 ई० से 232 हि०/847 ई०
10. मुतवक्किल - 232 हि०/847 ई० से 247 हि०/861 ई०
पतनकाल
11. मुन्तसिर बिल्लाह - 247 हि०/861 ई० से 248 हि०/862 ई०
12. मुसतईन बिल्लाह - 248 हि०/862 ई० से 252 हि०/866 ई०
13. मोतिज़ बिल्लाह - 252 हि०/866 ई० से 255 हि०/869 ई०
14. मुहतदी बिल्लाह - 255 हि०/869 ई० से 256 हि०/870 ई०
15. मोतमिद - 256 हि०/870 ई० से 279 हि०/892 ई०
16. मोतज़िद बिल्लाह - 279 हि०/892 ई० से 289 हि०/902 ई०
17. मुक्तफ़ी बिल्लाह - 289 हि०/902 ई० से 295 हि०/908 ई०
18. मुक़्तदिर बिल्लाह - 295 हि०/908 ई० से 320 हि०/932 ई०
19. क़ाहिर बिल्लाह - 320 हि०/932 ई० से 322 हि०/934 ई०
20. राज़ी बिल्लाह - 322 हि०/934 ई० से 329 हि०/940 ई०
21. मुत्तक़ी - 329 हि०/940 ई० से 333 हि०/944 ई०
पराधीनता काल
334 हिं०/946 ई० से 547 हि०/1152 ई०
स्वाधीनता काल
547 हि०/1152 ई० से 656 हि०/1258 ई०
अध्याय-11
बग़दाद का उत्थान - 2
अब्बासी ख़िलाफ़त का ज़माना मुसलमानों की सभ्यता और संस्कृति के उत्थान का ज़माना है। अब्बासी ख़िलाफ़त हालाँकि बनी उमय्या की ख़िलाफ़त के मुक़ाबले में कम विस्तृत थी, क्योंकि अन्दलुस (स्पेन) और मराकश अब्बासियों के प्रभुत्व से बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बासी ख़िलाफ़त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत या सियासी संगठन था। कहा जाता है कि एक बार हारून रशीद ने बादल के एक टुकड़े को गुज़रते हुए देखकर कहा, "तू चाहे कहीं चला जा, लेकिन बरसेगा मेरी ही सल्तनत के अन्दर।" यह कुछ इस क़िस्म की बात है, जैसी मौजूदा शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ी सल्तनत के सम्बन्ध में कही जाती थी कि सूरज अंग्रेज़ी सल्तनत में कहीं नहीं डूबता।
(1) बनी अब्बास का ज़माना युद्ध-विजय का ज़माना नहीं था। इस ज़माने में नए-नए इलाक़े फ़तह नहीं हुए। बात यह है कि इस्लामी हुकूमत इतनी विस्तृत हो गई थी कि इसे सँभाल पाना ही मुश्किल था। सिन्ध नदी से अटलांटिक महासागर तक पाँच हज़ार मील का फ़ासला है। उस ज़माने में जब कि हवाई जहाज़, रेलें और मोटरें नहीं थीं, यह फ़ासला बहुत ज़्यादा था। लोग या तो पैदल या घोड़ों पर सफ़र करते थे और एक छोर से दूसरे छोर तक कई-कई महीनों में पहुँचते थे। इस ज़माने में भी यदि सिन्धु नदी से मराकश तक रेल चलने लगे तो इसके द्वारा भी भारत का एक यात्री एक हफ़्ते से पहले मराकश नहीं पहुँच सकता।
इस विस्तृत और विशाल सल्तनत में तुर्क, पठान, सिन्धी, ईरानी, कुर्द, अरब, मिस्री, बर्बर और अंदुलुसी (स्पेनी) आदि अनगिनत क़ौमों रहती थीं। इस्लाम, ईसाइयत, बौद्धमत, हिन्दू-मत, यहूदियत आदि तमाम धर्मों के माननेवाले इस्लामी सल्तनत में रहते थे। स्पष्ट है कि ऐसी विशाल एवं विस्तृत और विभिन्न प्रकार के लोगों से भरी हुई सल्तनत को सँभालना आसान काम नहीं था। इसलिए अब्बासियों का ध्यान साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा सल्तनत में शान्ति व्यवस्था क़ायम करने की ओर रहा। इसके अतिरिक्त मुसलमानों का जोशे जिहाद और वह ताज़ा जोश जो इस्लाम के प्रारंभ में पैदा हो गया था, ठंडा पड़ा गया था। मुसलमान अब कठिन जीवन के बदले आराम का जीवन गुज़ारने के आदी होने लगे थे। अब्बासियों का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने मुल्क की ख़ुशहाली में बढ़ोतरी की और ज्ञान एवं कला का विकास किया।
अब्बासी ख़िलाफ़त की सीमा में अरब, ईरानी, तुर्क, रूमी, मिस्री, हबशी, बर्बर और हिन्दुस्तानी यानी अनगिनत क़ौमें निवास करती थीं। इन तमाम क़ौमों के मेलजोल से एक नई सभ्यता ने जन्म लिया जो अपने समय की सबसे उत्कृष्ट एवं विकसित सभ्यता थी और हालाँकि इस मेलजोल के कारण मुसलमान ग़ैर इस्लामी मूल्यों से प्रभावित हुए, परन्तु आधिपत्य इस्लामी मूल्यों का रहा, जिसके कारण यह सभ्यता एक इस्लामी सभ्यता कहलाती है।
वैसे अब्बासियों के ज़माने में कुछ युद्ध भी हुए। यह युद्ध रूमियों से हुए। पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि मुसलमानों ने शाम (सीरिया), मिस्र और एशिया-ए-कोचक का बड़ा हिस्सा रूमियों से ले लिया था, परन्तु रूमी सल्तनत उस प्रकार ख़त्म नहीं हुई थी, जिस प्रकार ईरानी सल्तनत ख़त्म हो गई थी। इसके कारण मुसलमानों से उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अब्बासियों की सल्तनत हालाँकि बनी उमय्या के मुक़ाबले में छोटी थी, लेकिन उनका एक बड़ा फ़ौजी कारनामा यह है कि उन्होंने रूमियों को इतनी शिकस्त दी कि अन्ततः उन्होंने मुसलमानों का आधिपत्य स्वीकर कर लिया और हर साल 'ख़िराज' देने लगे। मुसलमानों को रूमियों पर ऐसा आधिपत्य उमवी दौर में भी प्राप्त नहीं हुआ था।
(2) अब्बासी ख़िलाफ़त बनी उमय्या की तरह एक शुद्ध अरब ख़िलाफ़त नहीं थी। इस दौर में ईरानी, तुर्क और दूसरी क़ौमें भी विभिन्न हैसियतों से हुकूमत में सम्मिलित हो गईं। ख़लीफ़ा और उसका ख़ानदान अरब था, प्रशासन व्यवस्था में ईरानियों का ज़ोर था और फ़ौज में तुर्कों की अधिकता थी। हालाँकि इन क़ौमों को इस्लाम के हित से ज़्यादा ख़लीफ़ा का हित प्यारा था, लेकिन इनके अन्दर एकता की बुनियाद इस्लाम ने ही डाली थी और ख़लीफ़ा इस्लाम ही के नाम पर काम करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब्बासी ख़िलाफ़त अरब ख़िलाफ़त नहीं, बल्कि इस्लामी ख़िलाफ़त थी।
परन्तु इस ऊपरी एकता और एकजुटता के अन्दर नस्ली, क़बाइली एवं क्षेत्रीय संकीर्णता पूर्ववत काम कर रही थी। बल्कि ये संकीर्णताएँ जो बनी उमय्या ने उभारी थीं, बनी अब्बास के काल में पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गईं। अब्बासियों ने अपने लाभ के लिए अरबों को अरबों से लड़वाया और दूसरी ओर ग़ैर अरबों को अरबों के विरुद्ध भड़काया।
बनी उमय्या के काल में अरबों की संकीर्णता के कारण ग़ैर अरबी जातिवाद की जो आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही थी, बनी अब्बास के काल में वह पूरी शक्ति से भड़क उठी और उसने मात्र अरबी संकीर्णता के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी इस्लाम विरोध का एक मोर्चा क़ायम कर दिया। यह मात्र जातिवादी आन्दोलन नहीं था, बल्कि इसके साथ-साथ ज़ंदक़ा (इस्लाम-दुश्मनी) और नास्तिकता के कीटाणु भी थे।
जातिवादी आन्दोलन का प्रारंभ तो इस बहस से हुआ कि अरबों को ग़ैर अरबों पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है, परन्तु बहुत जल्द इसने अरबों के विरोध का रंग अपना लिया और अरबों की आलोचना यहाँ तक की कि क़ुरैश सहित उनके एक-एक क़बीले की आलोचना में किताबें लिखी जाने लगीं। कट्टरपंथी ग्रुप अरबों की निन्दा से बढ़कर ख़ुद इस्लाम पर हमले करने लगे और ग़ैर अरब हाकिमों ने उनका प्रोत्साहन किया।
ज़ंदक़ा (इस्लाम-दुश्मनी) मात्र आस्था की गुमराहियों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यावहारिक रूप में नैतिक सीमा से आज़ादी भी उसके साथ अनिवार्य थी। शराबनोशी, बलात्कार, रिश्वत आदि ज़ंदक़ा के लिए अनिवार्य थे।
(3) अब्बासी हुकूमत भी उमवी हुकूमत की तरह मुलूकियत (राजतंत्र) थी और सच्चे अर्थों में ख़िलाफ़त नहीं थी। यहाँ भी बाप के बाद बेटा या उसका कोई निकट सम्बन्धी बादशाह बनता था। मुलूकियत (राजतन्त्र) का अन्त और ख़िलाफ़त के पुनरुत्थान की कोशिश का ख़याल अब मुसलमानों के सियासी दृष्टिकोण से लगभग समाप्त हो चुका था। यही कारण है कि इस दौर में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) की तरह किसी ने ख़िलाफ़त के पुनरुत्थान की कोशिश नहीं की। अब ख़िलाफ़त के पुनरुत्थान का मतलब यह समझा जाने लगा कि यदि मुलूकियत शासन-प्रणाली में तबदीली लाए बिना हुक्मरानों को इस्लामी आदेशों पर अमल करने के लिए मना लिया जाए तो इसे ख़िलाफ़त का पुनरुत्थान कहा जा सकता है। जनता में सही इस्लामी हुकूमत की स्थापना की जो इच्छा थी उससे प्रारंभिक अब्बासी ख़लीफ़ाओं ने पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया और लोगों को यक़ीन दिलाया कि वे सही इस्लामी हुकूमत क़ायम करेंगे। अतः जब सफ़्फ़ाह के हाथ पर कूफ़ा में बैअत हुई तो सफ़्फ़ाह के अलावा उसके चाचा दाऊद बिन अली ने लोगों को यक़ीन दिलाया कि :
"हम इसलिए नहीं निकले हैं कि अपने लिए सोना-चाँदी जमा करें या महल बनाएँ और नहरें खोदकर लाएं। हम जिस चीज़ के लिए आगे आए हैं वह यह है कि हमारा हक़ छीन लिया गया था और हमारे चाचा की औलाद (अबू तालिब की औलाद) पर ज़ुल्म किया जा रहा था और बनी उमय्या तुम्हारे बीच बुरे तरीक़ों पर चल रहे थे। तुम्हारे बैतुलमाल में से ग़लत ढंग से ख़र्च कर रहे थे। अब हमपर तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) का ज़िम्मा है कि हम तुम्हारे बीच अल्लाह की किताब (क़ुरआन) और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सीरत (हदीस) के अनुसार हुकूमत करेंगे।"
परन्तु न्याय पर आधारित इस्लामी हुकूमत क़ायम करने का यह वादा सिर्फ़ वादा ही रहा। बनी अब्बास ने बनी उमय्या से जिस अत्याचार से बदला लिया, वह ऐसा कर्म है जो कभी इस्लामी नहीं कहा जा सकता। ख़ुरासान के फ़क़ीह (इस्लामी विधान के ज्ञाता) इबराहीम बिन मैमून (रहमतुल्लाह अलैह) ने अब्बासियों का इसलिए साथ दिया था कि उन्होंने किताब (क़ुरआन) एवं सुन्नत के अनुसार हुकूमत क़ायम करने का वादा किया था, परन्तु जब अब्बासियों की कामयाबी के बाद उन्होंने अबू मुस्लिम ख़ुरासानी से अल्लाह के आदेशों को स्थापित करने की माँग की और किताब (क़ुरआन) व सुन्नत (हदीस) के ख़िलाफ़ काम करने पर टोका तो अबू मुस्लिम ने उन्हें क़त्ल करवा दिया।
इसमें संदेह नहीं कि बाद के अब्बासी हुक्मरानों ने इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम किया, इस्लामी क़ानून लागू करने में दिलचस्पी ली, लेकिन इस हुकूमत की भी बुनियादी ख़राबी यही थी कि वह मुलूकियत (राजतंत्र) थी। उनके हाथों जो इंक़िलाब हुआ उससे सिर्फ़ हुक्मरान ही बदले, शासन-प्रणाली नहीं बदली। उन्होंने उमवी काल की किसी एक ख़राबी को भी दूर नहीं किया, बल्कि उन तमाम विकृतियों को ज्यों का त्यों बरक़रार रखा जो ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद मुलूकियत (राजतंत्र) के आ जाने से इस्लामी शासन-व्यवस्था में घुस गए थे। बादशाही का तर्ज़ वही रहा जो बनी उमय्या ने अपना रखा था। फ़र्क़ सिर्फ़ यह हुआ कि बनी उमय्या के लिए क़ुस्तनतीनिया के 'क़ैसर' नमूना थे तो अब्बासी ख़लीफ़ाओं के लिए ईरान के 'किसरा'।
अब हर बात बादशाह के तरीक़े पर निर्भर थी। बादशाह जितना अच्छा और बुरा मुसलमान होता था, उसके किए गए कामों में उसी अनुपात से इस्लाम की झलक नज़र आती थी। ख़ानदानी बादशाहत का उसूल अब पूरी तरह छा गया था। मंसूर और नफ़्स ज़किया में ख़िलाफ़त के हक़ के मसले पर जो लम्बा पत्र व्यवहार चला, उससे ज़ाहिर होता है कि एक सौ पचास साल के अन्दर-अन्दर मुसलमानों की मानसिकता में कितना बदलाव आ गया था। ख़ानदान, क़बीला और नस्ल पर गर्व, जिसकी इस्लाम ने जड़ काट दी थी, अब वही अन्ध-संकीर्णताएँ फिर उभर आई थीं। इस पत्र-व्यवहार से ज़ाहिर होता है कि दावते हक़ (सच्चाई को स्थापित करने का) किसी का मक़सद नहीं था। दोनों पक्षों ने सबसे ज़्यादा ज़ोर अपने-अपने ख़ानदान की श्रेष्ठता और महानता साबित करने पर दिया। मंसूर को यदि हम नज़रअन्दाज़ भी कर दें तो भी आश्चर्य होता है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (नफ़्स ज़किया) जो हज़रत हसन (रज़ियल्लाहु अन्हु) की औलाद में से थे, वह इस फ़ित्ने (बुराई) का किस प्रकार शिकार हो गए। हालाँकि एक समय वह था जब हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ख़लीफा बन जाने पर अबू सुफ़ियान (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) को यह कहकर वरग़लाना चाहा था कि हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनका हक़ मार लिया है तो हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जवाब दिया था—
"तुम्हारी यह बात इस्लाम और अहले इस्लाम (इस्लाम के अनुयायी) की दुश्मनी की दलील है।"
(4) अब्बासी काल के मआशरे पर जब हम नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि आलिमों के असर व रसूख़ और मज़हब से दिली लगाव के बावजूद समाज में अनैतिक एवं ग़लत सरगर्मियों में उमवी काल के बाद और बढ़ौतरी हुई। इस्लाम से पूर्व ईरान में ज्योतिषियों और भविष्यवाणी करनेवालों की बड़ी अहमियत थी। न केवल आम जनता उनसे अपने भाग्य का हाल मालूम करती थी, बल्कि बादशाह और आलिम भी अपने फ़ैसले ज्योतिषियों की सलाह के बिना नहीं करते थे। विभिन्न चीज़ों से अच्छे-बुरे शगुन लिए जाते थे। इस्लाम ने यह कहकर कि अल्लाह के अतिरिक्त भाग्य का हाल कोई नहीं बता सकता, ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं के पेशे पर चोट लगाई थी, लेकिन जब अब्बासी ख़िलाफ़त पर ईरानियों का प्रभाव बढ़ा तो ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं का यह कारोबार फिर चमक उठा और यह बीमारी इस्लामी दुनिया में ऐसी फैली कि अब तक इसके प्रभाव मौजूद हैं।
दास-प्रथा उस काल में भी थी। हालाँकि इस्लाम में सिर्फ़ जंग होने पर ग़ुलाम बनाने की इजाज़त थी, लेकिन इस काल में ग़ुलामी-प्रथा ने बाक़ायदा कारोबार का रूप ले लिया और मात्र ग़ुलाम बनाने के लिए सरहदी इलाक़ों में छापे मारे जाने लगे। ग़ुलामों के कारोबार और व्यापार में यहूदी सबसे आगे थे, लेकिन अब ख़ुद मुसलमानों ने भी इस कारोबार को अपना लिया जो इस्लाम के बिलकुल विपरीत काम था। अब तमाम बड़े इस्लामी शहरों में बाक़ायदा बाज़ार लगने लगे जहाँ लौंडी-ग़ुलाम (दासी-दास) को बेचा जाता था। बहरहाल ग़ुलामी के रिवाज के बावजूद यह भी हक़ीक़त है कि ग़ुलामों से वह दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था जिसकी मिसालें रूमा के प्राचीन इतिहास और अमेरिका के नवीन इतिहास में मिलती हैं। इस्लामी दुनिया में ग़ुलामों के साथ सद्व्यवहार किया जाता था और यह ग़ुलाम उच्च से उच्च पदों पर पहुँचते थे और लौंडियाँ हुक्मरानों की माएँ बन जातीं थीं। मामून रशीद और मोतसिम जैसे महान हुक्मरान लौंडियों के पेट से जन्मे थे। संगीत और चित्रकारी ने भी इस काल में सरकारी सरपरस्ती में तरक़्क़ी की।
जानदार चीज़ों की तस्वीर बनाना, बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) के सदृश्य होने के कारण इस्लाम ने वर्जित क़रार दिया था। इसी लिए मुसलमान चित्रकारों और कलाकारों ने अपने कला की अभिव्यक्ति के लिए जानदार चीज़ों के चित्र के बदले ख़ुशनवीसी (सुलेख) करने, बेलबूटे और प्राकृतिक दृश्यों का चित्र बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। अब्बासी ख़िलाफ़त के बाद इस कला का बहुत विकास हुआ और यह मुसलमानों की विशेष कला के रूप में जानी जाने लगी। लेकिन अब्बासी काल में उमवी काल की तरह इसकी मिसालें मिलती हैं कि इनसानी तस्वीर बनाने का रिवाज मुसलमानों में प्रारंभ हो गया। हम यह नहीं जानते कि ये तस्वीरें मुसलमान बनाते थे या ग़ैर मुस्लिम, लेकिन मालूम होता है कि मुसलमान हुक्मरानों ने उन्हें नापसन्द नहीं किया।
अब्बासी काल में इनसानी तस्वीर बनाने से ज़्यादा जिस ग़ैर इस्लामी कला ने तरक़्क़ी पाई वह संगीत था। शराब, औरत और संगीत का चोली-दामन का साथ रहा है। ग़ैर इस्लामी समाज में इन तीनों चीज़ों के बिना जीवन आनन्द रहित समझा जाता है। मुसलमान हुक्मरान इनमें से सबसे पहले संगीत की ओर आकर्षित हुए और उसके बाद नबीज़ (खजूर का शरबत) के बहाने शराब और लौंडी के पर्दे में औरत की ख़्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। बहरहाल अब्बासी काल में शराबनोशी इतनी सीमित थी कि हम उस काल के समाज को यूरोप और अमेरिका की तरह शराबी समाज नहीं कह सकते और वैश्यावृत्ति की लानत से भी मुस्लिम समाज अभी तक पाक था, लेकिन संगीत अपनी सारी मधुरता के साथ दरबार में विशेषकर अमीरों एवं रईसों में आम तौर पर रिवाज पा चुका था। [इस जगह यह हक़ीक़त सामने रखना चाहिए कि मुसलमानों में ग़ैर इस्लामी रस्म और परम्परा शाही दरबार के रास्ते से आई। यदि ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद मुलूकियत की शासन-प्रणाली क़ायम न होती तो हुकूमत पर अवाम का अंकुश बना रहता और जनता के समक्ष जवाबदेही के भय से हुक्मरान ग़ैर इस्लामी तरीक़े आसानी से नहीं अपना सकते थे।]
इबराहीम मौसली (742 ई० से 804 ई०) और इस्हाक़ मौसली (767 ई० से 850 ई०) इस काल के सबसे बड़े संगीतकार थे। इसहाक़ मौसली के बारे में मोतसिम कहा करता था कि जब इसहाक़ गाता है तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है जैसे कोई नया मुल्क फ़तह हो गया हो।
उस काल की महिलाओं में दो नाम सबसे नुमायाँ नज़र आते हैं। एक हारून रशीद की बीवी मलिका ज़ुबैदा जो अमीन रशीद की माँ थी और दूसरी सैयदा नफ़ीसा (मृत्यु - 824 ई०) जो मिस्र की एक धर्म-परायण औरत थीं। राबीया बसरी के साथ जो उमवी काल में थीं, मुसलमान सैयद नफ़ीसा को भी ओलिया-अल्लाह जैसी हस्तियाँ समझते हैं। मलिका ज़ुबैदा (762 ई० से 831 ई०) ने अपने जन-कल्याणकारी कामों के कारण बड़ा नाम कमाया। मक्का की प्रसिद्ध नहर 'नहर ज़ुबैदा' जिसके कारण मक्का में पानी की ज़रूरत सदियों तक पूरी होती रही और अब भी पूरी होती है, इसी इनसान दोस्त औरत की कोशिशों से बनी।
(5) अब्बासी काल की प्रशासन-व्यवस्था बहुत हद तक वैसी ही थी जैसी बनी उमय्या के काल में थी। सिर्फ़ एक बड़ी तबदीली हुई थी, और वह यह कि वज़ीर (प्रधानमन्त्री) का नया पद क़ायम किया गया था जो उमवी दौर में नहीं था। अब वज़ीर, सल्तनत के तमाम कामों का ज़िम्मेदार होता था और वह सिर्फ़ ख़लीफ़ा के समक्ष जवाबदेह होता था। कातिब और हाजिब के पद उस दौर में भी क़ायम थे। पुलिस विभाग भी क़ायम था। इसका सबसे उच्च अधिकारी साहिबे शुरता कहलाता था, जिसे आज के परिभाषिक शब्द में इन्सपेक्टर जनरल पुलिस कहा जा सकता है। शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त आम जनता के आचरण और चाल-चलन की निगरानी, मंडियों और बाज़ारों में वस्तुओं की क़ीमतों पर नज़र रखना और नाप-तौल की निगरानी भी साहिबे शुरता की ज़िम्मेदारी थी। शराबनोशी, जुआ और इसी प्रकार की अन्य सामाजिक बुराइयों की रोक-थाम भी साहिबे शुरता के ही कर्त्तव्य में सम्मिलित थी।
पूरी सल्तनत विभिन्न प्रान्तों में बँटी हुई थी जिनकी सीमाएँ बदलती रहती थीं। इस काल में पहली बार केन्द्रीय ख़िलाफ़त के तहत अर्द्ध-सम्प्रभु हुकूमतें भी क़ायम की गईं। इनमें उत्तरी अफ़्रीक़ा की अग़लिबी हुकूमत थी जिसका केन्द्र क़ैरवान था और दूसरी ख़ुरासान की ताहिरी हुकूमत थी जिसका केन्द्र नेशापुर था। [इस हुकूमत का संस्थापक मामून रशीद का ईरानी सिपहसालार ताहिर था जिसको मामून रशीद ने 205 हि०/820 ई० में ख़ुरासान का स्थायी गवर्नर नियुक्त किया था। ताहिर के बाद उसकी औलाद हुक्मरान हुई। मुतवक्किल के इंतिक़ाल के बाद इस हुकूमत ने संप्रभुता प्राप्त कर ली थी। ताहिरी ख़ानदान के हुक्मरानों में ताहिर के लड़के अब्दुल्लाह ने अपनी दानशीलता, बुद्धिमत्ता, विवेक और प्रजा के हित के प्रयासों के कारण बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। अब्दुल्लाह बिन ताहिर अपने कारनामों के लिहाज़ से बरामिका से किसी प्रकार कम नहीं था। ताहिरी हुकूमत 259 हि०/872 ई० में ख़त्म हो गई]
न्याय व्यवस्था भी लगभग वही थी जो उमवी काल में थी। अब्बासी काल के क़ाज़ियों ने भी इनसाफ़ और न्याय के दामन को कभी नहीं छोड़ा। हुक्मरान क़ाज़ियों के फ़ैसले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। महदी ने अपने महल में एक अलग अदालत क़ायम की थी और आम एलान करवाया था कि जिसके साथ कोई अन्याय हुआ हो वह उसके सामने मुक़द्दमा पेश करे। एक बार क़ाज़ी ने ख़ुद महदी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दिया था। हारून रशीद के ज़माने में अदालती व्यवस्था उस समय ज़्यादा व्यवस्थित हो गई थी जब क़ाज़ी अबू यूसुफ़ को ख़लीफ़ा की पूरी सल्तनत का प्रधान क़ाज़ी (चीफ़ जस्टिस) बनाया गया। उस समय से क़ाज़ियों के लिए एक विशेष पोशाक जिसमें जुब्बा और अमामा होते थे, निर्धारित किया गया।
फ़ौजी संगठन भी बड़ी हद तक उमवी काल की भाँति थी। हर दस सिपाही पर एक अरीफ़ और सौ पर एक क़ाइद होता था। सौ सिपाहियों का दस्ता 'जमाअत' और दस जमाअत का दल 'करदोस' कहलाता था। फ़ौजी संगठन और फ़ौज की तादाद मोतसिम के ज़माने में सबसे ज़्यादा थी।
नेज़ा (भाला), तलवार, तीर-कमान, ख़ोद (सिर में पहननेवाला सुरक्षा कवच), ज़िरह और मिनजनीक़ (गोले दाग़नेवाला हथियार) ख़ास हथियार थे। घेराव के समय मिनजनीक़ के अलावा जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थीं वे 'अरादे', 'दबाबे' और 'कबाश' कहलाती थीं। उन्हें क़िले या चार दीवारी दरवाज़ा को टक्कर मारकर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घेराव के दौरान पिचकारी से एक प्रकार का तेल जो 'नफ़त' कहलाता था, फेंका जाता, उसके बाद अंगारे और आग फेंकी जाती थी जिससे दुश्मन के क़िले में आग लग जाती थी। इंजीनियरों की एक बड़ी जमाअत जो 'महंदसीन' कहलाती थी, हर घेराव में फ़ौज के साथ होती थी। हथियार और घोड़े आम तौर पर सरकारी ख़ज़ाने से उपलब्ध कराए जाते थे।
अब्बासी काल में समुद्री-बेड़ा भी बहुत मज़बूत था, परन्तु समुद्री शक्ति के असली मालिक क़ैरवान के अग़लिबी हुक्मरान थे जिन्होंने न केवल सक़लिया टापू को फ़तह किया था बल्कि जिनका बेड़ा मध्य रूम सागर की सबसे बड़ी ताक़त बन गया था।
(6) इस काल में कृषि में भी तरक़्क़ी हुई। बनू अब्बास की कृषि-व्यवस्था भी क़रीब-क़रीब वही थी जो उमवी काल में थी। यानी ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा ख़लीफ़ा, शाही ख़ानदान, मन्त्रियों और उच्च अधिकारियों के क़बज़े में था। सरकारी सेवाओं के लिए परिश्रम के रूप में ज़मीनें जागीर की शक्ल में दे दी जाती थीं। महदी के ज़माने में ज़मीनों के मापने और उसकी व्यवस्था करनेवाला विभाग क़ायम हुआ और पूरी सल्तनत की ज़मीनों को मापा गया। कोशिश यह होती थी कि किसानों के साथ अन्याय न हो सके, इनपर टैक्स ज़्यादा न हो और इसकी वसूली में ज़ुल्म और जब्र से काम न लिया जाए। हारून रशीद ने क़ाज़ी अबू यूसुफ़ से 'किताबुल-ख़िराज' इसी उद्देश्य के लिए लिखवाई थी। मिस्र और इराक़ में उस समय दुनिया का सबसे बड़ा 'जल संसाधन विभाग' क़ायम था। जिस प्रकार मिस्र को 'तोहफ़-ए-नील' (नील नदी का तोहफ़ा) कहा जाता है उसी प्रकार इराक़ दजला और फ़ुरात का पुरस्कार है।
अतः मुक़द्दसी ने लिखा है—
"ईराक़ स्वयं कोई ज़रख़ेज़ (उपजाऊ) या साधनों से भरपूर राज्य नहीं है। इसकी अज़मत और ख़ुशहाली का दारोमदार दजला और फ़ुरात और हिन्द महासागर से होनेवाले व्यापार पर निर्भर है।"
इराक़ और मिस्र के इस जल संसाधन-व्यवस्था की अब्बासी काल में न केवल पहले की भाँति पूरी-पूरी देखभाल की गई बल्कि नई-नई नहरें निकालकर उसका विस्तार भी किया गया। मिस्र और इराक़ के अतिरिक्त ख़ूज़िस्तान, सीस्तान और मरू के क़रीब मरग़ाब नदी की वादी में भी नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी जिसने इन इलाक़ो को इराक़ और मिस्र की तरह दुनिया के सबसे हरे-भरे और उपजाऊ क्षेत्रों में बदल दिया था। बसरा अपनी खजूरों के लिए और ख़ूज़िस्तान अपने गन्ने और शकर के लिए सारी दुनिया में मशहूर था। नींबू और संतरे की खेती उसी काल में इस्लामी दुनिया में शुरू हुई। ये फल हिन्दुस्तान से लाए गए थे।
(7) चौथी सदी हिजरी के प्रसिद्ध पर्यटक मुक़द्दसी ने इराक़ के बारे में, जो अब्बासी ख़िलाफ़त का हृदय समझा जाता था, लिखा है—
"यह सुसभ्य, सुसंस्कृत लोगों और आलिमों का केन्द्र है। इसमें वह विशाल शहर बसरा है जिसे दुनिया कहा जा सकता है। यहीं बग़दाद है जिसकी सारी दुनिया में प्रशंसा होती है। यहीं कूफ़ा और सामरा जैसे सुन्दर और महत्त्वपूर्ण शहर बसाए गए। इराक़ में गर्व करने लायक़ इतनी चीज़ें हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। [अनुमान लगाया गया है कि अब्बासी ख़िलाफ़त की उन्नति के काल में बग़दाद की आबादी 25 लाख थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर था।]
इस्लामी दुनिया की राजधानी बग़दाद भी इराक़ में थी। इसे 'सलामती का शहर' कहा जाता था। मुक़द्दसी ने बग़दाद की प्रशंसा में लिखा है—
“यहाँ के नागरिक अच्छा पोशाक पहननेवाले और सभ्य हैं। वे सुबुद्धि और विवेकशील हैं। उनमें ज्ञान की गंभीरता है। हर बढ़िया और उत्तम चीज़ यहाँ है। हर कला और ज्ञान के विशेषज्ञ यहाँ से निकलते हैं। यह शहर हर प्रकार के फ़ैशन का घर है।"
ख़लीफ़ा मंसूर ने शहर को दजला के पश्चिमी तट पर गोलाकार रूप में आबाद किया था। चारों तरफ़ फ़सील थी जिसमें चार दरवाज़े थे। यानी बाबुल-कूफ़ा, बाबुल-बसरा, बाबुल-शाम और बाबुल ख़ुरासान। शहर एक बाक़ायदा नक़्शे के तहत आबाद किया गया था। मध्य में शाही महल और जामा मस्जिद थी और यहाँ से हर दिशा में सीधी-सीधी सड़कें निकलती थीं। बाद में शहर पूर्वी तट पर भी फैल गया। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरिया पर कश्ती के कई पुल थे। नहरों की अधिकता के कारण पानी की कमी नहीं थी और बाग़ों-उद्यानों की बहुलता थी। जहाँ नहरों के गन्दे होने की संभावना थी वहाँ उन्हें ऊपर से ढक दिया गया था। कर्ख़ का मुहल्ला जो चार मील लम्बा और दो मील चौड़ा था, न केवल बग़दाद का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। यहाँ हर चीज़ के बाज़ार अलग-अलग थे। काग़ज़ और किताबों के बाज़ार भी थे।
बग़दाद में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। यहाँ के कारीगर विभिन्न प्रकार के रेशमी कपड़े, बारीक मलमल और ऊनी चादरें बनाने में बड़े प्रसिद्ध थे। मलमल सुन्दरता और बारीकी में अपनी मिसाल आप थी। यह कहावत मशहूर थी कि यदि किसी को सुन्दर और बारीक कपड़े की ज़रूरत हो तो इराक़ पहुँचे। गहने, चमड़े, सुगंधित तेल, इत्र, साबुन और शीशा उद्योग ने बग़दाद में विशेष रूप से तरक़्क़ी की थी।
बग़दाद में बाग़ों की अधिकता, शानदार महलों और कोठियों के अलावा पोलो खेलने का मैदान भी था और बाद में एक चिड़ियाघर भी बन गया था। दरिया के किनारे चूँकि ठंड रहती थी इसलिए कश्ती की सैर अमीरों (उच्च अधिकारियों) और आम लोगों की ख़ास दिलचस्पी थी। अमीर लोग गर्मियों का समय तहख़ाना में गुज़ारते थे। पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था जो उत्तर के पहाड़ों से लाई जाती थी।
कूफ़ा— रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। विशेषकर यहाँ के अमामे यानी पगड़ियाँ सारी इस्लामी दुनिया में पसंद की जाती थीं। वाद्य-यन्त्र, हथियार, ज़ेवर और चमड़े के उद्योग भी तरक़्क़ी पर थे। मिट्टी के बरतन और गुलदान, जिनपर तरह-तरह के बेल-बूटे बने होते थे, का उद्योग कूफ़ा का प्रमुख उद्योग था। मुक़द्दसी ने लिखा है—
“यहाँ का पानी अच्छा, इमारतें सुन्दर, बाज़ार शानदार और चारों ओर खजूर के बाग़ हैं और सबसे सही अरबी भाषा कूफ़ा में बोली जाती है।"
अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान काल में कूफ़ा शहर बग़दाद के समान समझा जाता था।
बसरा— बसरा के सम्बन्ध में मुक़द्दसी ने लिखा है—
“यह शहर नहर उबल्ला के साथ-साथ फैला हुआ है। मुझे बग़दाद के मुक़ाबले में बसरा ज़्यादा पसन्द है क्योंकि यहाँ आर्थिक सहूलतें ज़्यादा हैं। हमाम (स्नानगृह) अच्छे हैं, ज्ञान और कला तरक़्क़ी पर हैं और व्यापार विकसित है।"
बसरा वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र था। पूर्वी क्षेत्र का सारा माल बसरा के रास्ते इराक़ में आता था। यहाँ के व्यापारी दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते थे। वे तमाम चीज़ें जिनके लिए कूफ़ा मशहूर था, बसरा में भी बनाई जाती थीं।
इराक़ के दूसरे उद्योग जो बग़दाद, बसरा और कूफ़ा लगभग हर शहर में मौजूद थे निम्नलिखित हैं—
क़ालीन उद्योग - क़ालीन ऊनी होते थे जिनमें रेशम की मिलावट होती थी। यह क़ालीन फ़र्श पर बिछाने के अलावा दीवारों पर लटकाए भी जाते थे। क़ालीन पर बेल-बूटों के अलावा जानवरों की तस्वीरें बनाने का रिवाज भी हो गया था।
शीशा उद्योग – आईना-निर्माण और शीशे के बरतनों के उद्योग ने भी अब्बासी काल में बड़ी तरक़्क़ी की। बरतनों पर जानवरों की तस्वीर भी बनाई जाती थी। हालाँकि शीशा उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र शाम (सीरिया) था लेकिन इराक़ में भी यह उद्योग तरक़्क़ी पर था और यहाँ के बनाए हुए क़ंदील, झाड़-फ़ानूस और जाम (गिलास) दूर-दूर तक जाते थे।
लौह उद्योग - लोहे के उद्योग में हथियार बनाने के अलावा कुर्सी, बरतन, तराज़ू, बाट, बक्से, छुरी-चाक़ू, विज्ञान और गणित के औज़ार शामिल थे। मौसिल (Mosul), ज़ंजीर, चाक़ू और छुरी उद्योग के लिए और हर्रान गणित एवं विज्ञान में काम आनेवाले उपकरणों और तराज़ू उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे।
लकड़ी उद्योग - लकड़ी उद्योग में कश्ती बनाना सबसे प्रमुख उद्योग था। इराक़ के बढ़ई 36 प्रकार की कश्ती बनाते थे। उबल्ला कश्ती-निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र था।
इराक़ के शहरों के अलावा क़ैरवान, स्कंदरिया, फ़िस्तात, दमिश्क़, इस्फ़हान, रै, नेशापुर, हरात, बुख़ारा, ख़्वारिज़्म और समरक़ंद भी बड़े-बड़े शहर थे, जिनमें से कुछ बसरा और कूफ़ा से कम नहीं थे। यह सभी शहर उद्योग-धन्धे और व्यापार का केन्द्र थे और अब्बासी काल में इनमें ज्ञान-विज्ञान एवं वैचारिक सरगर्मी भी पूरे ज़ोर-शोर से शुरू हो गई थी।
(8) दजला और फ़ुरात व्यापारिक मार्गों का काम करते थे। बसरा हालाँकि इराक़ की सबसे बड़ी बंदरगाह थी लेकिन बड़े समुद्री जहाज़ सीधे बग़दाद तक जा सकते थे। इसके बाद छोटी कश्तियाँ इस्तेमाल की जाती थीं। जो जहाज़ चीन जाते थे वे ज़्यादा बड़े होते थे। उनके पेंदे की सतह पानी से इतनी ऊँची होती थी कि उनपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती थीं जिसमें दस-दस पायदान होते थे।
रूम, चीन और भारत से व्यापारिक सम्बन्ध क़ायम थे। भारत से हाथी दाँत, आबनूस की लकड़ी और संदल, और चीन से काग़ज़, दवात, सोने-चाँदी के बरतन और रेशमी कपड़े मँगाए जाते थे। उत्तरी देशों यानी रूस, क़फ़क़ाज़ और आरमीनिया से व्यापार का केन्द्र मौसिल था। इस शहर के विषय में मुक़द्दसी ने लिखा है—
“यहाँ इमारतें दिलकश, हवा अच्छी, पानी उम्दा, बाज़ार अच्छे और सराएँ आरामदेह हैं। कई सैर-सपाटे की जगहें भी हैं। मौसिल ज़ंजीर, चाक़ू-छुरी, फल और अचार, मुरब्बा के उद्योग में प्रसिद्ध था।"
समुद्री व्यापार का एक दूसरा बड़ा केन्द्र सीराफ़ की बन्दरगाह थी। यह शहर अब्बासी काल में इतना आबाद और इमारतें इतनी मनमोहक और बाज़ार इतने सुन्दर थे कि लोग सीराफ़ को बसरा से भी अच्छा समझते थे। सागवान और ईंट की बनी ऊँची-ऊँची कोठियाँ थीं जिनमें एक-एक की क़ीमत पचास-पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा थी। सीराफ़ की बंदरगाह चीन से आने-जानेवाले जहाज़ों का सबसे बड़ा केन्द्र था।
अरब प्रायद्वीप में अदन और सुहार के बन्दरगाह बड़े अहम थे। अदन यमन देश का सबसे बड़ा केन्द्र था। यहाँ से जहाज़ एक ओर भारत और चीन तक और दूसरी ओर पूर्वी अफ़्रिक़ा के दक्षिणी बंदरगाहों तक जाते थे। बाहर से आनेवाला सामान हिजाज़ के रास्ते या लाल सागर के मार्ग से मिस्र और फिर वहाँ से मराकश जाता था। मुक़द्दसी ने लिखा है—
"अदन एक ख़ुशहाल शहर है। याक़ूत, चमड़े, चीते की खाल और ग़ुलामों की मंडी है यहाँ एक ख़ास क़िस्म का कपड़ा बनता है।"
बंदरगाह सुहार के सम्बन्ध में मुक़द्दसी ने लिखा है—
“हिन्द महासागर के किनारे इससे अधिक बड़ा शहर दूसरा नहीं है। यहाँ दौलत और तिजारत यमन के शहर ज़ुबैद और सनआ से ज़्यादा है। मकान ईंट और सागौन के हैं। बाज़ार में रौनक़ रहती है। भारत और चीन के जहाज़ यहाँ आते हैं। शहर में एक नहर है। अकाल के समय यमन की अनाज की ज़रूरत इसी शहर से पूरी की जाती है। ईरानी छाए हुए हैं और फ़ारसी आम ज़बान है।"
9. ज्ञान और कला एवं लेखन जिसका प्रारंभ बनी उमय्या के दौर में हो गया था, इस दौर में बहुत विकसित हुए। यूनानी, फ़ारसी सुरयानी और संस्कृत की किताबों के बहुत अधिक अनुवाद किए गए। इस काल में अत्यधिक लेखन का एक कारण यह भी था कि मुसलमान काग़ज़ बनाने की कला सीख गए थे। यह कला उन्होंने उन चीनी क़ैदियों से सीखी जो बनी उमय्या के काल में समरक़ंद की विजय के समय 704 हि०/1304 ई० में गिरफ़्तार हुए थे। इससे पहले किताबें झिल्लियों, खालों और विभिन्न प्रकार के पत्तों पर लिखी जाती थीं।
अध्याय-12
बौद्धिक एवं साहित्यिक दुनिया
बनी अब्बास के हालात पढ़कर मालूम हो गया होगा कि यह काल युद्ध, विजय एवं साम्राज्य विस्तार का काल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं साहित्यिक विकास का काल था। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बनी अब्बास का काल देश-विजय का काल नहीं था, बल्कि बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विजय का काल था। बग़दाद की श्रेष्ठता इतिहास में इस कारण नहीं है कि वह हारून रशीद और मामून रशीद जैसे हुक्मरानों की राजधानी थी, बल्कि बग़दाद की श्रेष्ठता इसलिए है कि वह अपने काल में ज्ञान एवं कला और सभ्यता एवं संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा केन्द्र था। उस काल के आलिम जब तक बग़दाद आकर बड़े-बड़े विद्वानों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेते थे, तब तक वे अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं समझते थे। यहाँ इस्लामी दुनिया के दूर-दराज़ इलाक़ों से आलिम, साहित्यकार और कवि शिक्षा प्राप्त करने भी आते थे और इसलिए भी आते थे कि उनका यहाँ सम्मान होता था।
बग़दाद के अलावा बसरा और कूफ़ा के शहर भी उस काल में ज्ञान के बहुत बड़े केन्द्र थे। मिस्र में ऐसा ही एक केन्द्र फ़िस्तात में था। बनी अब्बास के अन्तिम काल में क़ैरवान, रै, नेशापुर, मरू और बुख़ारा भी ज्ञान एवं साहित्य के बड़े केन्द्र बन गए थे।
धार्मिक ज्ञान
इस्लामी हुकूमत का जब प्रारंभ हुआ तो शुरू-शुरू में शिक्षा मौखिक (ज़बानी) रूप से दी जाती थी। बनी उमय्या के अन्तिम काल से किताबों के लिखने का काम प्रारंभ हो गया, परन्तु लेखन का काम बनी अब्बास के काल में पूरे ज़ोर-शोर से शुरू हुआ। मुसलमान आलिमों ने सबसे पहले दीनी शिक्षा और धार्मिक ज्ञान की ओर ध्यान दिया। क़ुरआन की तफ़सीरें (व्याख्या) लिखी गईं। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेश और उनकी बातें, जो हदीस' कहलाती हैं, जमा की गईं। फ़िक़्ह (इस्लामी विधान) की भी किताबें लिखी गईं। उन किताबों में बताया गया है कि जब कोई नया मसला पेश आए तो क़ुरआन और हदीस की रौशनी में उसे कैसे हल किया जाए। फ़िक़्ह के आलिम को 'फ़क़ीह' और हदीस के आलिम को 'मुहद्दिस' कहा जाता है। तफ़सीर, हदीस और फ़िक़्ह के अलावा इतिहास, साहित्य और कविता पर भी किताबें लिखी गईं और अन्त में दर्शन-शास्त्र, खगोल-शास्त्र, गणित, चिकित्सा आदि पर किताबें लिखी गईं। ये विषय मुसलमानों के लिए नए थे, इसलिए पहले इन विषयों की दूसरी भाषाओं में जो किताबें थीं उनका अनुवाद किया गया। फिर मुसलमानों ने इन विषयों पर ख़ुद किताबें लिखीं।
अब्बासी काल में जो आलिम और साहित्यकार पैदा हुए उनपर मुसलमानों को गर्व है और वे इतने बड़े हैं कि आज तक उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। हमें आज इस्लाम के सम्बन्ध में जो मालूमात हैं, वह उन्हीं की लिखी हुई किताबों से हैं और तमाम इस्लामी ज्ञान की बुनियाद यही किताबें हैं।
फ़िक़्हे इस्लामी या इस्लामी विधान का संकलन और हदीस की प्रमाणिक किताबों का लेखन अब्बासी काल का महान इल्मी कारनामा है। फ़िक़्ह के एतिबार से वे चार मस्लक जो सबसे ज़्यादा सम्मानित हुए, इसी काल से सम्बन्ध रखते हैं। वे चार मस्लक हैं : फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ई और फ़िक़्ह हंबली। इनके अलावा फ़िक़्ह जाफ़री भी जिसपर असना-अशरी शीआ अमल करते हैं, इसी काल में संकलित हुआ। फ़िक़्ह के इन मस्लकों को प्रारंभ करनेवाले आलिम निम्न हैं :
इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह)
(80 हि०/699 ई० से 150 हि०/767 ई०)
नोमान बिन साबित, जो इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से मशहूर हुए, कूफ़ा के रहनेवाले थे और कपड़े का व्यापार करते थे। उन्होंने जिस इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद रखी वह फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम से मशहूर है। इमाम अबू हनीफ़ा बड़े अच्छे अख़लाक़वाले और दौलतमंद आदमी थे। वह अपनी दौलत से शागिर्दों की मदद किया करते थे। वह किसी की ग़ीबत (परोक्ष निंदा) नहीं करते थे और अपना काम ईमानदारी पूर्वक पूरा करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कपड़ा ख़रीदा, उस कपड़े में कुछ ख़राबी थी। इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) ने उस ख़राबी को छुपाया नहीं और ख़रीदार से कहा कि इस ख़राबी को जानने के बाद अगर तुम ख़रीदना चाहो तो ख़रीद लो।
वह अपने रुपये से शागिर्दों की मदद भी किया करते थे, उनके एक शागिर्द मुहम्मद बहुत ग़रीब थे और इमाम अबू हनीफ़ा के पास आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार उनके बाप आए और मुहम्मद को घर ले गए और उनसे कहा कि अबू हनीफ़ा तो पैसेवाले हैं, वह हर वक़्त पढ़ सकते हैं। परन्तु तुम ग़रीब हो। यदि पढ़ने में ही सारा वक़्त गुज़ार दोगे तो कमाकर खाओगे कैसे। अपने बाप की इसी हिदायत के बाद मुहम्मद कई दिनों तक इमाम अबू हनीफ़ा के पास पढ़ने नहीं गए। जब वह पढ़ने आए तो इमाम अबू हनीफ़ा ने उनसे ग़ैर-हाज़िर होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मैं ग़रीब हूँ और रोज़ नहीं आ सकता। इस पर इमाम साहब ने उन्हें एक थैली दी कि जब इसमें पैसे ख़त्म हो जाएँ तो फिर ले जाना। इस प्रकार मुहम्मद ने अपने उस्ताद की मदद से इतना इल्म हासिल किया कि इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों में सबसे आगे निकल गए और लोग उन्हें इमाम मुहम्मद कहने लगे।
फ़िक़्ह हनफ़ी का सबसे अधिक प्रसार इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों क़ाज़ी अबू यूसुफ़ (113 हि०/731 ई० से 183 हि०/799 ई०) और इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी (132 हि०/749 ई० से 189 हि ०/805 ई०) के कारण हुआ। क़ाज़ी अबू यूसुफ़ ने सबसे पहले फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें लिखीं। उन्हें चूँकि हारून रशीद ने पूरी ख़िलाफ़ते अब्बासिया का चीफ़ जस्टिस बनाया था इसलिए उनके कारण फ़िक़्ह हनफ़ी का बहुत प्रसार हुआ। परन्तु फ़िक़्ह हनफ़ी की वास्तविक बुनियाद इमाम मुहम्मद की लिखी किताबों पर है। वे पहले ग़ुलाम थे, फिर आज़ाद हो गए थे। उन्होंने पच्चीस से ज़्यादा किताबें लिखी थीं। शहर 'रै' में जब उनका इंतिक़ाल हुआ तो ख़ुद हारून रशीद ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और बड़े अफ़सोस से कहा, “आज इल्मे फ़िक़्ह ज़मीन में दफ़न हो गया।”
इमाम मुहम्मद अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रथम संस्थापक समझे जाते हैं। अत: पेरिस और रूम के क़ानूनविदों ने 1389 हि०/1969 ई० में उनकी बारह सौवीं पुण्यतिथि (बर्सी) बड़ी श्रद्धा से मनाई।
फ़िक़्ह हनफ़ी के माननेवालों की तादाद इस समय सबसे ज़्यादा है। चीन, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान और अफ़ग़ान और तुर्क मुसलमान आम तौर पर हनफ़ी मत को माननेवाले हैं।
इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह)
(93 हि०/711 ई० से 179 हि०/795 ई०)
इस काल के एक महान आलिम इमाम मालिक (93 हि० से 179 हि०) हैं। इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ा में थे और इमाम मालिक लगभग उसी ज़माने में मदीना में थे। वे मदीना में रहने के कारण हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीसों के अपने ज़माने में सबसे बड़े आलिम थे। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) ने हदीसों का एक संकलन भी तैयार किया था, जिसका नाम 'मुवत्ता' था। इस वक़्त हदीसों की जितनी किताबें हैं, मोवत्ता उनमें सबसे पुरानी है।
इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) भी इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) की तरह लोगों की मदद करते थे। उन्हें ख़लीफ़ा की तरफ़ से जो तोहफ़े मिलते थे वे उन्हें लोगों में बाँट दिया करते थे। इमाम मालिक बड़े ईमानदार और उसूल के पक्के थे। वे अपने उसूल के मुक़ाबले में बड़े से बड़े इनसान के सामने झुकने से इनकार कर देते थे।
एक बार ख़लीफ़ा हारून रशीद मदीना आया और उसने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि वे महल में आकर 'मुवत्ता' कि किताब उसके लड़कों को पढ़ा दें। इमाम मालिक ने महल में जाने से मना कर दिया और कहा कि जिसे पढ़ने का शौक़ हो उसे ख़ुद आना चाहिए। इसपर हारून रशीद अपने दोनों बेटों अमीन और मामून को लेकर इमाम साहब के पास आया। वहाँ बहुत-से लड़के पढ़ रहे थे। यह देखकर ख़लीफ़ा ने कहा, "इस भीड़ को अलग कर दीजिए।" इमाम मालिक ने जवाब दिया, "दो-चार के कारण इतने सारे विद्यार्थियों का नुक़सान नहीं किया जा सकता।" और इस प्रकार हारून रशीद और उसके लड़कों को तमाम विद्यार्थियों के साथ पढ़ना पड़ा। मुवत्ता पढ़ने के बाद इमाम मालिक ने ख़लीफ़ा को मदीना के फ़क़ीरों और ग़रीबों की ओर ध्यान दिलाया और हारून ने उनकी हिदायत पर सभी फ़क़ीरों को रुपया बाँटा।
फ़िक़्ह मालिकी की सबसे अहम किताब 'मद्दव्वना' है जो क़ैरवान के क़ाज़ी और फ़ातेहे सक़लिया असद बिन फ़रात (मृत्यु 213 हि०/828 ई०) और इमाम सहनून (मृत्यु 240 हि०/854 ई०) ने संपादित की थी। आजकल उत्तरी और पश्चिमी अफ़्रीक़ा के मुसलमान अधिकतर फ़िक़्ह मालिकी ही पर अमल करते हैं। अंदलुस (स्पेन) के मुसलमान भी इसी फ़िक़्ह पर अमल करते थे।
इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह)
(150 हि०/767 ई० से 204 हि०/820 ई०)
इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) के शागिर्द मुहम्मद बिन इद्रीस, जो इमाम शाफ़ई के नाम से मशहूर हैं, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने तक़रीबन एक सौ किताबें लिखी थीं जिनमें से बहुत-सी अब भी मौजूद हैं। इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) की ज़िन्दगी का अधिकतर समय मक्का, मादीना, बग़दाद और मिस्र में गुज़रा और आख़िर में मिस्र में ही इंतिक़ाल किया। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) के बाद वे अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे। वे बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी गिनती अरबी भाषा में सबसे अच्छे लेखकों में होती है। 'किताबुल-उम' और 'अल-रिसाला' उनकी बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं। अल-रिसाला का उर्दू में अनुवाद हो चुका है।
इमाम शाफ़ई के फ़िक़्ह का प्रसार उन महान आलिमों की कोशिशों का नतीजा है जो पाँच सौ साल तक मिस्र, अरब, शाम (सीरिया), इराक़ और ईरान में पैदा होते रहे। उस ज़माने में इस विशाल भू-भाग में जितने महान आलिम हुए हैं, उनमें अधिकतर शाफ़ई थे। आजकल इंडोनेशिया, मलेशिया, हिजाज़, मिस्र व शाम और उत्तरी अफ़्रीक़ा के अधिकतर मुसलमान फ़िक़्ह शाफ़ई के अनुयायी हैं। इस्लामी दुनिया में फ़िक़्ह हनफ़ी के बाद सबसे ज़्यादा अनुयायी फ़िक़्ह शाफ़ई के हैं।
इमाम अहमद बिन हम्बल (रहमतुल्लाह अलैह)
(164 हि०/780 ई० से 241 हि०/855 ई०)
इस दौर के चौथे बड़े आलिम इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल (रहमतुल्लाह अलैह) हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल (रहमतुल्लाह अलैह) अपने ज़माने में हदीस के सबसे बड़े आलिम थे। उन्होंने 'मुसनद' के नाम से हदीसों की एक बहुत बड़ी किताब लिखी, जिसमें लगभग चालीस हज़ार हदीसें हैं। इमाम शाफ़ई की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल भी ग़रीब थे। उन्हें ख़लीफ़ा और प्रशासन की ओर से हज़ारों रुपये मिलते थे, लेकिन वे उसमें से अपने ऊपर कुछ भी ख़र्च नहीं करते थे। यह सारी रक़म लोगों में बाँट देते थे।
ख़लीफ़ा मोतसिम ने एक बार उनपर बड़ी सख़्ती की। वह चाहता था कि एक बात, जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ग़लत समझते थे, उनसे मनवा ले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसपर ख़लीफ़ा ने उन्हें कोड़ों से इतना पिटवाया कि वे बेहोश हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने यह सभी अत्याचार सहन कर लिए, परन्तु जिस बात को वे ग़लत समझते थे उसे उन्होंने सही नहीं कहा। उनकी क़ुरबानियों के कारण उन्हें सारी इस्लामी दुनिया में ऐसी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि वे दिलों के बादशाह बन गए। जब उनका बग़दाद में इंतिक़ाल हुआ तो आठ लाख से ज़्यादा लोग जनाज़े में शरीक थे। इतने लोग कभी बड़े से बड़े बादशाह के जनाज़े में भी शरीक नहीं हुए।
अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन काल में फ़िक़्ह हम्बली के माननेवालों का बग़दाद में बड़ा ज़ोर था। परन्तु अब सिर्फ़ अरब के सूबा नज्द में उनकी अक्सरियत है। हम्बली फ़िक़्ह के माननेवाले आलिमों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि 'इमाम इब्ने तैमिया' ने प्राप्त की, जिनकी चर्चा आगे चलकर होगी।
फ़िक़्ह जाफ़री के संस्थापक इमाम जाफ़र सादिक़ (80 हि०/699 ई० से 148 हि०/765 ई०) हैं, जिनकी चर्चा उमवी काल में हो चुकी है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक दोनों इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द रह चुके थे। पाकिस्तान, भारत, ईरान और इराक़ के शिआ नागरिक फ़िक़्ह जाफ़री पर अमल करते हैं।
इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह)
(194 हि०/810 ई० से 256 हि०/870 ई०)
इस काल के मुहद्दिसों में मुहम्मद बिन इसमाईल जो इमाम बुख़ारी के नाम से मशहूर हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं। उन्होंने हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेशों और उनकी ज़िन्दगी की घटनाओं को बड़ी खोजबीन के बाद एक किताब में जमा किया। यह किताब 'सहीह बुख़ारी' कहलाती है। इस किताब के लिखने में इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) की ज़िन्दगी के तीस साल लगे। यह हदीसों की इतनी सही किताब है कि मुसलमान इसे क़ुरआन के बाद दुनिया की सबसे सही किताब समझते हैं। इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) उस ज़माने के अन्य बहुत-से आलिमों की तरह व्यापार किया करते थे। वे बहुत दौलतमंद थे, लेकिन सादा ज़िन्दगी गुज़ारते थे और अपने रुपए से दूसरों की मदद किया करते थे।
इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) ने 'सहीह हदीसों' का यह संकलन हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंतिक़ाल के लगभग ढाई सौ साल बाद तैयार किया। इससे पहले इमाम मालिक भी 'मुवत्ता' के नाम से हदीसों का एक प्रमाणिक संकलन तैयार कर चुके थे, जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंतिक़ाल के डेढ़ सौ साल बाद तैयार किया गया था, परन्तु इससे यह समझना कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बाद डेढ़ सौ साल तक हदीसों की कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, सही नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि हदीसों को लिखने का काम ख़िलाफ़ते राशिदा ही के ज़माने में प्रारंभ हो गया था और सौ साल के अन्दर-अन्दर ख़ुद सहाबा की ज़िन्दगियों में अनगिनत संकलन तैयार हो गए थे और आलिम मसजिदों में उनका दर्स दिया करते थे, लेकिन चूँकि उस ज़माने के लोग याद कर लेने को लिखने के मुक़ाबले में ज़्यादा अच्छा तरीक़ा समझते थे, इसलिए यह किताबें मशहूर नहीं हुईं। इसके अलावा इन किताबों में हर प्रकार की हदीसें मौजूद थीं। वे हदीसें भी जिनको सही समझा जाता था और वे भी जिनके सही होने में शक था। दर्स देनेवाले आलिम तो सही-ग़लत का फ़र्क़ समझा देते थे, परन्तु संकलनों में सही-ग़लत को पहचानना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) और बाद के मुहद्दिसों ने इस मुश्किल को देखकर फ़ैसला किया कि उन हदीसों का एक संकलन तैयार किया जाए जो हर लिहाज़ से सही हों, यानी जिन्हें सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और उनके बाद आनेवाले बुज़ुर्ग एवं आलिम सही समझते आए हैं, ताकि इस प्रकार मुसलमान बिना किसी दिक़्क़त के हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सही आदेशों को मालूम कर सकें। सहीह बुख़ारी और हदीस की दूसरी किताबें जिनकी चर्चा आगे आएगी, इसी विचार से लिखी गईं।
सिहाहे सित्ता – हदीसों की एक और किताब 'सहीह मुस्लिम' भी इसी ज़माने में लिखी गई। यह इमाम मुस्लिम (रहमतुल्लाह अलैह) (202 हि०/821 ई० या 206 हि ०/821 ई० से 261 हि०/875 ई०) की लिखी हुई है और सहीह बुख़ारी के दर्जे की है।
इसी ज़माने में एक मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी (209 हि०/824 ई० से 279 हि०/893 ई०) ने जो इमाम बुख़ारी के शागिर्द थे, 'शमाइल' के नाम से एक किताब लिखी। इसमें सहीह हदीसों की मदद से हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी की घटनाएँ लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सहीह तिरमिज़ी' के नाम से हदीसों की एक किताब भी लिखी थी।
सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और सहीह तिरमिज़ी के अलावा इस ज़माने में हदीसों के तीन और प्रसिद्ध और प्रमाणिक संकलन तैयार किए गए जो अपने तैयार करनेवालों के नाम पर 'अबू दाऊद' (202 हि०/817 ई० से 275 हि०/888 ई०), 'इब्ने माजा' (209 हि०/824 ई० से 273 हि०/886 ई०) और 'नसई' (221 हि०/836 ई० से 303 हि०/915 ई०) कहलाते हैं। सहीह हदीसों की चूँकि ये कुल छ: किताबें हैं, इसलिए इन्हें 'सिहाहे सित्ता' यानी छः सही किताबें कहा जाता है। इस प्रकार इन किताबों को इस्लामी ज्ञान के समझने में बुनियादी अहमियत हासिल है।
मुहद्दिसों की इन किताबों में एक ओर दीनी मालूमात जमा कर दी गई हैं और दूसरी ओर उनमें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने की सही ऐतिहासिक घटनाएँ जमा कर दी गई हैं। इस प्रकार हदीस की ये किताबें दीन के काम भी आती हैं और इतिहास में भी इनसे मदद मिलती है। इनमें जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं वे इतिहास की किताबों के मुक़ाबले में ज़्यादा सही हैं।
इतिहास एवं भूगोल
इस काल में इतिहास एवं जीवन चरित्र की भी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गईं। इनमें एक इब्ने हिशाम (मृत्यु-213 हि०/828 ई०) की लिखी हुई ‘सीरतुन-नबी’ है। इसमें हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी की घटनाएँ लिखी गई हैं। परन्तु इस काल के सबसे बड़े जीवनी लेखक इब्ने साद (168 हि०/784 ई० से 230 हि०/845 ई०) हैं। इन्होंने 'तबक़ात' के नाम से एक बहुत बड़ी किताब लिखी है। इसमें हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अलावा उनके सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और सहाबा के बाद आनेवाले महान लोगों जिन्हें 'ताबईन' कहा जाता है, के हालात लिखे हैं। इस प्रकार 'तबक़ात इब्ने साद' से कई सौ महापुरुषों के हालात मालूम हो सकते हैं।
युद्ध-विजयों का हाल एक और इतिहासकार बलाज़ुरी (मृत्यु 279 हि०/892 ई०) ने अपनी किताब 'फ़ुतूहुल-बुलदान' में लिखा है। इस किताब में हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के काल की विजयों और उसके बाद अंदलुस (स्पेन), मध्य ऐशिया और सिन्ध आदि की विजयों का उल्लेख किया है।
परन्तु इस काल के सबसे बड़े इतिहासकार इब्ने जरीर तबरी (224 हि०/839 ई० से 310 हि०/923 ई०) हुए हैं। उन्होंने चौदह वृहत भागों में इतिहास की एक किताब लिखी है, जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने से अपने ज़माने तक तीन सौ वर्ष का इतिहास विस्तार से लिखा है। तबरी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क़ुरआन की एक बहुत बड़ी तफ़सीर भी लिखी है। इन दो किताबों के अलावा वे कई बड़ी-बड़ी किताबों के लेखक हैं। तबरी इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े लेखक हैं। उन्होंने जितनी किताबें लिखीं, आज तक किसी ने नहीं लिखीं। कहा जाता है कि वे प्रत्येक दिन चौदह पृष्ठ लिखा करते थे और यह सिलसिला ज़िंदगी भर जारी रहा।
मसऊदी
इस काल के लेखकों में मसऊदी (मृत्यु-345 हि०/956 ई०) का नाम भी उल्लेखनीय है। वह इतिहासकार होने के अलावा एक बड़े भूगोलशास्त्री और महान पर्यटक भी थे। मसऊदी बग़दाद के रहनेवाले थे। उन्होंने 305 हि०/917 ई० से कुछ पहले इस शहर से अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले वे ईरान गए। वहाँ से पाकिस्तान आए। सिन्ध और मुल्तान की सैर की। फिर वे भारत के पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ कोंकण और मालाबार के इलाक़े की सैर करते हुए श्रीलंका पहुँचे। जब वे श्रीलंका पहुँचे तो उन्हें बग़दाद से निकले हुए तीन वर्ष हो चुके थे। यहाँ से वे एक तिजारती क़ाफ़िले के साथ चीन गए। चीन से वापसी पर उन्होंने ज़ंजबार का रुख़ किया और पूर्वी अफ़्रीक़ा के समुद्री तटों की सैर करते हुए मेडगास्कर पहुँचे। यहाँ से दक्षिणी अरब और अम्मान होते हुए अपने वतन बग़दाद वापस आ गए।
अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराने ज़माने में जबकि कोई हवाई जहाज़, रेलें, और मोटरें नहीं थीं और एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बिलकुल अनभिज्ञ होते थे, सफ़र करना कितना कठिन होता होगा। विशेषकर समुद्र का सफ़र तो बहुत ही ख़तरनाक होता था। छोटे-छोटे जहाज़ों की समुद्र की तूफ़ानी लहरों के आगे क्या हक़ीक़त थी, लेकिन इस बहादुर पर्यटक ने इल्म और मालूमात हासिल करने के लिए इन तमाम ख़तरों का मुक़ाबला किया और अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया के एक बड़े हिस्से की सैर कर डाली और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखकर इन विभिन्न देशों की सभ्यता एवं संस्कृति से लोगों को परिचित कराया।
मसऊदी ने सफ़र की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए एक जगह लिखा है :
"मैंने चीन, रूम, क़ुलज़म और यमन के समुद्रों में सफ़र किया है। इन समुद्री सफ़रों के बीच मुझे तरह-तरह के ख़तरों से इतना अधिक मुक़ाबला करना पड़ा कि मैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं कर सकता। लेकिन पूर्वी अफ़्रीक़ा और भारत के बीच समुद्र में मैंने जो कुछ देखा वह आज भी याद है। यहाँ मुझे बेहद ख़ौफ़नाक और कठिन क्षणों से गुज़रना पड़ा। यहाँ मैंने एक ऐसी मछली देखी जो एक सौ गज़ लम्बी है या उससे भी ज़्यादा। जहाज़ चालक उसे 'आवाल' कहते हैं। यह मछली समुद्र में कहीं न कहीं नज़र आ जाती है और जब उसका एक पर कहीं नज़र आता है तो यूँ लगता है, जैसे किसी डूबते हुए जहाज़ का बादबान है। यह मछली कभी-कभी सिर निकालकर इतने ज़ोर से साँस लेती है कि पानी आसमान की ओर तीर की तरह निकलता है। दिन हो या रात जहाज़ के चालकों के लिए यह एक समस्या बनी रहती है और वे उसे भगाने के लिए ख़ौफ़नाक आवाज़ोंवाले गोले छोड़ते रहते हैं।"
मसऊदी ने जिस मछली का उल्लेख किया है वह संभवतः वही मछली है जिसे आजकल ह्वेल कहा जाता है।
बग़दाद वापस पहुँचने के बाद मसऊदी को फिर सफ़र के शौक़ ने बेचैन कर दिया। अब उन्होंने ऐशिया-ए-कोचक का रुख़ किया और वहाँ से शाम और फ़िलस्तीन की सैर करते हुए मिस्र पहुँचे। वह शायद उसके बाद भी सफ़र करते और उत्तरी अफ़्रीक़ा और अंदलुस (स्पेन) आदि जाते, लेकिन उनकी ज़िन्दगी ने साथ नहीं दिया और मिस्र पहुँचने के कुछ साल बाद शहर फ़िस्तात में उनका इंतिक़ाल हो गया।
मसऊदी बीस से अधिक किताबों के लेखक थे, परन्तु मात्र दो किताबों के अब उनकी और कोई किताब नहीं मिलती। उन किताबों के नाम 'मुरव्वजुज़-ज़ह्ब' और 'अल-तंबीह वल-अशराफ़' हैं। मसऊदी की किताबों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें पढ़कर चौथी सदी हिजरी की ज़िन्दगी आईना के समान हमारे सामने आ जाती है और उस काल की सभ्यता एवं संस्कृति का नक़्शा खिंच जाता है। यह बात उस ज़माने के किसी इतिहासकार में नहीं मिलती।
अबुल हसन अशअरी
इस काल के आलिमों में अबुल हसन अशअरी (260 हि०/873 ई० से 324 हि०/935 ई०) का नाम भी उल्लेखनीय है। ईरानियों और दूसरी ग़ैर अरब क़ौमों के मुसलमान हो जाने के कारण एवं ग़ैर मुस्लिम नागरिकों के साथ मेलजोल और उनकी किताबों के अरबी में अनुवाद हो जाने के कारण, उस काल के मुसलमानों में ग़ैर इस्लामी विचारधारा फैलनी शुरू हो गई थी। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ई आदि ने इन विचारधाराओं की रोकथाम की, परन्तु इन गुमराह करनेवाली विचारधाराओं का बौद्धिक स्तर पर जिसने कामयाब मुक़ाबला किया वह इमाम अबुल हसन अशअरी हैं। उन्होंने पहली बार बौद्धिक आधार पर इस्लामी आस्थाओं और सिद्धान्तों की सच्चाई साबित की और एक नए इल्म की बुनियाद डाली जो इल्मे कलाम (तर्कशास्त्र) कहलाता है। जिसका उद्देश्य बौद्धिक दलीलों से इस्लाम की सच्चाई साबित करना है। वह लगभग ढाई सौ किताबों के लेखक थे जिनमें 'अल-इबाना' और 'मक़ालातुल इस्लामिईन' बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं।
विज्ञान
अब्बासी काल में दीनी उलूम (धार्मिक ज्ञान) के अलावा दूसरे उलूम जैसे चिकित्साशास्त्र, गणित, ख़गोलशास्त्र, रसायनशास्त्र, दर्शनशास्त्र और अन्य विषयों ने भी तरक़्क़ी की। इन विषयों का ज्ञान मुसलमानों ने पहली बार यूनानी, संस्कृत और दूसरी भाषाओं से अरबी में अनुवाद की हुई किताबों से सीखा, परन्तु जल्द ही वे इन विषयों पर इस प्रकार हावी हो गए कि जैसे ये उनके अपने विषय हों। उन्होंने इस मामले में रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इस हदीस पर अमल किया— “हिकमत (विज्ञान का ज्ञान) मुसलमानों की खोई हुई मीरास है, इसलिए वह जहाँ मिले हासिल कर लो।"
अतः मुसलमानों ने इन विषयों में ऐसी-ऐसी किताबें लिखीं कि आज भी वे अपने विषय की बुनियादी किताबें समझी जाती हैं। इन मुसलमान वैज्ञानिकों में से कुछ के नाम ये हैं :
मुहम्मद बिन मूसा ख़्वारिज़मी
मुहम्मद बिन मूसा ख़्वारिज़मी जिनका इंतिक़ाल (220 हि०/835 ई० या 230 हि०/844 ई०) में हुआ, इस काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित, बीजगणित और ख़गोलशास्त्र पर बड़ी मेयारी किताबें लिखीं और इन विषयों में नए अध्याय जोड़े। यूरोपवालों ने गिनती के अंकों और शून्य का प्रयोग उन ही की किताबों से सीखा।
मेकेनिक यानी विभिन्न यन्त्र बनाने की कला को तीन भाइयों ने जो बनू मूसा बिन शाकिर कहलाते थे, बड़ी तरक़्क़ी दी और इन विषयों में ऐसी किताबें लिखीं जो पहले कभी नहीं लिखी गईं। मामून रशीद के काल में भूमंडल की माप इन्हीं भाइयों ने की थी, जिनके नाम अहमद, हसन और मुहम्मद थे। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जाबिर बिन हय्यान (मृत्यु 161 हि०) भी इसी काल में हुआ। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उसे आधुनिक रसायन शास्त्र का संस्थापक कहा है। रसायनशास्त्र पर उसने जो किताबें लिखीं वे एक हज़ार पृष्ठों पर फैली हुई हैं और यूरोप में छप गई हैं। यूरोप में आधुनिक काल से पहले जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जाबिर की उन किताबों से फ़ायदा उठाया और यही कारण है कि जाबिर को आधुनिक रसायनशास्त्र का संस्थापक कहा गया है।
चिकित्साशास्त्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मुहम्मद बिन ज़करिया राज़ी (240 हि०/854 ई० से 320 हि०/932 ई०) ने प्राप्त की। राज़ी न केवल इस्लामी इतिहास में सबसे बड़े चिकित्सक माने गए हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सकों और डॉक्टरों में गिने जाते हैं। उन्होंने चिकित्साशास्त्र पर जो किताबें लिखीं उनका बाद में यूरोप की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और उनकी मदद से यूरोप ने चिकित्सा का ज्ञान सीखा।
दर्शनशास्त्र में याक़ूब किन्दी और फ़ाराबी (259 हि०/873 ई० से 339 हि०/950 ई०) ने प्रसिद्धि प्राप्त की। किन्दी ख़लीफ़ा मामून रशीद और उसके उत्तराधिकारियों के काल में था और पहला अरब-दार्शनिक समझा जाता है। फ़ाराबी ने दर्शन-शास्त्र को और तरक़्क़ी दी और 'मुअल्लिम सानी' (द्वितीय गुरु) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुअल्लिम अव्वल (प्रथम गुरु) अरस्तु को समझा जाता है जो प्राचीन काल में यूनान का सबसे बड़ा दार्शनिक था। किन्दी और फ़ाराबी की किताबों ने भी यूरोप के दार्शनिकों को प्रभावित किया।
साहित्य
साहित्य के विकास के लिहाज़ से भी अब्बासी काल को एक उच्च स्थान प्राप्त है। शब्दकोष और व्याकरण का जन्म इसी काल में हुआ। इस विषय के सबसे बड़े विद्वान और लेखक ख़लील नहवी (100 हि०/718 ई० से 175 हि०/791 ई०), सीबवैह (मृत्यु - 177 हि०/793 ई०) और असमई (122 हि०/740 ई० से 216 हि०/831 ई०) थे। ये तीनों अरबी शब्दकोष और व्याकरण का प्रारंभ करनेवाले थे।
साहित्य में सबसे बड़े विद्वान जाहिज़ (160 हि०/775 ई० से 255 हि०/868 ई०) की है, जिन्हें अरबी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकारों में गिना जाता है। उनकी किताब 'अल-हैवान' उन चार किताबों में गिनी जाती है जिनपर अरबी साहित्य आधारित है। अरबी साहित्य के इन चार शाहकारों में से बाक़ी तीन भी इसी दौर में लिखे गए। यानी इब्ने क़ुतैबा (213 हि०/828 ई० से 276 हि०/889 ई०) की 'अदबुल-कातिब' और 'ऐवानुल-अख़बार' और मुबर्रद (210 हि०/826 ई० से 285 हि०/898 ई०) की 'अल-कामिल फ़िल-अदब'।
सादा लेखन-शैली, वैचारिक गंभीरता, कवियों जैसी मधुरता जाहिज़ के लेखन की विशेषताएँ हैं। वे नस्ल से हबशी थे और धार्मिक आस्था की दृष्टि से मुतज़िला (मुसलमानों का एक फ़िरक़ा)। इस काल के वे अकेले लेखक हैं जिन्होंने मुलूकियत (राजतन्त्र) की शासन-प्रणाली पर सख़्त चोटें कीं। उनकी किताबों में से 'किताबुल-हैवान' और 'किताबुल-बयान' ने प्रसिद्धि अर्जित की।
इब्ने क़ुतैबा की 'ऐवानुल-अख़बार' दस भागों में है। यह साहित्य का ऐसा नमूना है जिसका अनुकरण बड़े-बड़े साहित्यकारों ने किया। 'ऐवानुल-अख़बार' और मुबर्रद की 'अल-कामिल फ़िल-अदब' उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में मालूमात प्राप्त करने का बहुत अच्छा स्रोत हैं।
अरबी शायरी भी अपने चरम पर उसी काल में पहुँची। उमवी काल के तीन शायर अख़तल, जरीर और फ़रज़्दक़ का पीछे उल्लेख हो चुका है। ये तीनों अरबी के प्रथम श्रेणी के शायरों में गिने जाते हैं। परन्तु अब्बासी काल के शायर इन सबसे आगे बढ़ गए। उन शायरों में अबू तम्माम (180 हि०/796 ई० से 228 हि०/842 ई०), अबुल-अताहिया (130 हि०/748 ई० से 210 हि०/825 ई०), अबू नूवास (145 हि०/762 ई० से 196 हि०/813 ई०) और बुहतरी (204 हि०/820 ई० 284 हि०/897 ई०) सबसे प्रसिद्ध हैं। ये शायर या तो क़सीदागो थे यानी ख़लीफ़ा और प्रशासन के उच्चाधिकारियों की तारीफ़ में नज़्में कहते थे, या उन्होंने उस काल के भौतिकवादी जीवन का प्रतिनिधित्व किया। इनमें सिर्फ़ अबुल-अताहिया सबसे भिन्न था, क्योंकि उसका विषय दुनिया की क्षण भंगुरता और मानवीय नैतिकता था। उस काल में एक अब्बासी शहज़ादा इब्ने मुअतेज़ (247 हि०/861 ई० से 296 हि०/908 ई०) भी एक महान शायर था।
संक्षेप यह है कि अब्बासी काल में बड़े-बड़े विद्वान जिस बहुलता से गुज़रे हैं, इस्लामी इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती बल्कि आधुनिक काल को छोड़कर सारी दुनिया के इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती हमने सिर्फ़ कुछ के ही नाम लिखे हैं।
अध्याय-13
तस्बीह के दाने बिखर गए
अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान काल तक (247 हि०/861 ई०) अंदलुस (Andlus) और मराकश के छोटे-छोटे मुल्कों को छोड़कर शेष सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान और फ़रग़ाना (Fragana) से लेकर क़ैरवान तक अब्बासी ख़िलाफ़त के अधीन थी। गोया मुसलमान उस समय सियासी लिहाज़ से बहुत हद तक संगठित थे। परन्तु अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन के बाद इस संगठन और एकता का अन्त हो गया। जिस सूबेदार को जहाँ मौक़ा मिला वहाँ उसने आज़ाद हुकूमत क़ायम कर ली। इस प्रकार एक केन्द्रीय हुकूमत की जगह कई हुकूमतें क़ायम हो गईं। इनमें तीन बड़ी हुकूमतों का उल्लेख हम यहाँ करते हैं :
सामानी (261 हि०/874 ई० से 395 हि०/1005 ई०)
यह हुकूमत (261 हि०) में मावराउन-नहर (Transoxania) में क़ायम हुई। अपने बुज़ुर्ग असद बिन सामान के नाम पर यह ख़ानदान सामानी कहलाता है। नसर बिन अहमद बिन असद सामानियों की आज़ाद हुकूमत का पहला हुक्मरान है। मावराउन-नहर के अलावा वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान और ख़ुरासान भी इस हुकूमत में शामिल थे। इसकी राजधानी बुख़ारा थी। सामानियों ने 395 हि०/1005 ई० तक यानी कुल 134 साल हुकूमत की। इस अवधि में उनके दस हुक्मरान हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध और अच्छा हुक्मरान इसमाईल सामानी (279 हि०/892 ई० से 295 हि०/907 ई०) था। इसमाईल बड़ा नेकमिज़ाज और न्याय-प्रिय बादशाह था। एक बार उसे मालूम हुआ कि शहर 'रै' में जिस तराज़ू के बाट में ख़िराज (ज़मीन का टैक्स) की चीज़ें तौली जाती हैं, वह निर्धारित वज़न से ज़्यादा वज़नी है। इसमाईल ने तुरन्त तहक़ीक़ की। सूचना सही निकली। अत: इसमाईल ने सही वज़न निर्धारित कर दिया और आदेश दे दिया कि विगत वर्षों में लोगों से जितना ज़्यादा ख़िराज लिया गया है, वह वापस कर दिया जाए।
नसर द्वितीय का काल ज्ञान एवं साहित्य की सरपरस्ती के कारण प्रसिद्ध है और उसके लड़के नूह प्रथम को यह प्रमुखता प्राप्त है कि उसने बुख़ारा में एक विशाल पुस्तकालय क़ायम किया था, जिसमें हर विषय और विद्या के अलग-अलग कमरे थे। मशहूर चिकित्सक और दार्शनिक इब्ने सीना ने यहाँ की क़ीमती और नायाब किताबों की बड़ी प्रशंसा की है। नूह प्रथम के लड़के मंसूर प्रथम के बारे में पर्यटक इब्ने हैक़ल ने लिखा है कि वह अपने दौर का सबसे न्यायी बादशाह था।
सामानियों का एक बड़ा कारनामा ख़ानाबदोश तुर्क क़बीलों के हमले से अपनी रियासत की हिफ़ाज़त करना है। इस उद्देश्य के लिए उत्तरी सीमाओं पर जगह-जगह चौकियाँ क़ायम थीं, जिन्हें 'रिबात' कहा जाता था। यहाँ जिहाद के लिए हर समय फ़ौजी तैयार रहते थे।
इसी काल में तुर्कों में इस्लाम तेज़ी से फैला और चौथी सदी हिजरी के आख़िर तक पूर्वी तुर्किस्तान यानी काशग़र और उससे लगे हुए इलाक़े में और उत्तरी तुर्किस्तान से लेकर रूस में वाल्गा की वादी में इस्लाम फैल गया।
सामानी काल में ज्ञान एवं साहित्य की दिल खोलकर सरपरस्ती की गई, लेकिन इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि फ़ारसी भाषा की तरक़्क़ी है। अब तक मुसलमान जो भी किताब लिखते थे, वह अरबी में होती थी। जो लोग अरब नहीं थे, जैसे ईरानी और तुर्क, वह भी अरबी ही में किताबें पढ़ते और लिखते थे। ये लोग शायरी भी फ़ारसी और तुर्की के बजाय अरबी में ही करते थे। सामानी बादशाहों ने अब फ़ारसी ज़बान की सरपरस्ती शुरू कर दी, क्योंकि वे ख़ुद फ़ारसी बोलते थे। अतः फ़ारसी का पहला बड़ा शायर 'रोदकी' (मृत्यु-329 हि०/940 ई०), इसमाईल के पोते नसर (301 हि०/913 ई० से 331 हि०/942 ई०) के दरबार का शायर था। इसी ज़माने में तबरी के प्रसिद्ध इतिहास और क़ुरआन की तफ़सीर, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हो चुकी है, का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। प्रसिद्ध दार्शनिक 'फ़ाराबी' और 'इब्ने सीना' का भी प्रारम्भिक सम्बन्ध सामानी दरबार से था। आलिमों में इल्मे कलाम (तर्कशास्त्र) के विशेषज्ञ 'इमाम मंसूर मातरीदी' (मृत्यु 330 हि०/941 ई०) और सूफ़ियों में अबू नसर सिराज (मृत्यु 378 हि०/988 ई०) भी इसी काल से सम्बन्ध रखते हैं। इनकी लिखी हुई किताब 'अल-लमा' अरबी में है और इल्मे तसव्वुफ़ की बुनियादी किताबों में गिनी जाती है।
तीसरी और चौथी सदी हिजरी में मुसलमानों में पर्यटन और भ्रमण का शौक़ हो गया था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो वे पहले ही से दूर-दूर के मुल्कों में जाते थे परन्तु अब पर्यटन, भ्रमण और मालूमात हासिल करने के लिए भी सफ़र करने का शौक़ हो गया था। उस ज़माने में पर्यटन एवं भ्रमण में लोगों की जो दिलचस्पी थी उसका एक तत्कालीन शायर और पर्यटक 'इब्ने महलहल' ने अपने शेरों में बड़ी सुन्दरता से उल्लेख किया है, जिन्हें पढ़कर उस ज़माने के मुसलमानों में पाए जानेवाले पर्यटन के शौक़ का कुछ अंदाज़ा हो सकता है। उसके शेरों के भावार्थ ये हैं—
"हमने दुनिया के आश्यर्च और ज़माने की नई-नई बातें देखीं। हमने चीन से मिस्र और मिस्र से तन्जा तक लोगों के हालात मालूम किए। हम तो वे लोग हैं कि पृथ्वी और समुद्र हमारे क़दमों तले रौंदे गए हैं। हमारे क़दम बर्फ़ की ठंडक और रेत की गरमी से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे घोड़ों ने किस-किस घाट का पानी न पिया! जब पृथ्वी के एक हिस्से से हमारा जी भर गया तो हमने दूसरे का रुख़ किया।”
चौथी सदी हिजरी के पर्यटकों में तीन नाम प्रमुख हैं। एक असतख़री, दूसरा मुक़द्दसी और तीसरा इब्ने हौक़ल। [इब्ने हौक़ल 331 हि०/933 ई० में बग़दाद से रवाना हुआ और तीस साल तक इस्लामी दुनिया का सफ़र करता रहा। पूर्व में वह सिन्ध से मुल्तान तक आया और पश्चिम में सक़लिया, अंदलुस (स्पेन) और अफ़्रीक़ा की विशाल मरुभूमि के पार माली और घाना तक गया। आख़िर में उसने एक सफ़रनामा (यात्रा-वृत्तान्त) लिखा, जिसमें अपने सफ़र के दिलचस्प हालात लिखे।] उसके लेखों से पता चलता है कि ख़ुरासान और विशेषकर तुर्किस्तान ने उस काल में न केवल ज्ञान एवं साहित्य में बल्कि उद्योग-धंधे, व्यापार, कृषि और सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत तरक़्क़ी की और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक सभ्य देशों की पंक्ति में आ गया। मुक़द्दसी लिखता है—
"ख़ुरासान" और "मावराउन-नहर" (तुर्किस्तान) का क्षेत्र तमाम रियासतों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। देश धनी है और जीवन के संसाधनों से पूर्ण है। यहाँ हरे-भरे खेत, घने जंगल, नदी और खनिजों की खानें और फूलों के बग़ीचे हैं। लोग नेक, दानशील और मेहमानों का सत्कार करनेवाले हैं। न्याय और इनसाफ़ क़ायम है। न बुरे काम होते हैं, न ही पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं। देशभर में मदरसे हैं और यहाँ आलिम सभी देशों से ज़्यादा हैं। फ़क़ीहों (इस्लामी विधान के ज्ञाता) को बादशाह का दर्जा हासिल है और धार्मिक जीवन सीधे रास्ते पर है। यह मुसलमानों की एक ऐसी रियासत है जिसपर वे गर्व कर सकते हैं और इस्लाम का पौधा यहाँ हरा-भरा है। सामानी सुचरित्र हैं। लोगों में एक कहावत मशहूर है कि यदि कोई पेड़ सामानियों से बग़ावत पर उतारू हो जाए तो बिना सूखे नहीं रह सकता।"
समरक़ंद, बुख़ारा, ख़्वारिज़्म, बल्ख़, मरू, हरात, नेशापुर और रै सामनी रियासत के सबसे ख़ुशहाल शहर थे। इन शहरों के बारे में मुक़द्दसी ने लिखा है :
"सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में समरक़ंद से ज़्यादा फलता-फूलता कोई शहर नहीं। नेशापुर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है और इस्लामी दुनिया में उसका जोड़ नहीं। बल्ख़ जन्नते ख़ुरासान (ख़ुरासान की जन्नत) है। बग़ीचे शहर को घेरे हुए हैं और शहर के अधिकतर रास्तों के साथ नहरें और पानी के नल गुज़रते हैं। 'रै' सफ़ाई और ख़ूबसूरती में बेमिसाल है यहाँ आलिम बहुत हैं। कोई वाइज़ (धर्मोपदेशक) ऐसा नहीं जो क़ानूने इस्लाम से वाक़िफ़ न हो और कोई हाकिम ऐसा नहीं जो आलिम न हो। मोहतसिब सच्चाई के लिए मशहूर हैं। नगर के वक्ता के भाषणों में साहित्य की मिठास है। रै इस्लामी सभ्यता का एक ऐसा नमूना है जिसपर गर्व किया जा सकता है।"
आख़िर में सामानी हुकूमत भी अब्बासियों की तरह कमज़ोर होती गई। सूबेदार बाग़ी होने लगे और ख़ुरासान एवं ग़ज़नी के इलाकों में उनके एक सिपहसालार सुबग्तगीन ने अपनी आज़ाद हुकूमत क़ायम कर ली और बुख़ारा, समरक़ंद पर काशग़र के बादशाह ईलक ख़ानिया [ईलक ख़ानिया ख़ानदान की हुकूमत का काल 380 हि०/990 ई० से 609 हि०/1212 ई० तक है। यह शुद्ध तुर्क ख़ानदान था और इसकी राजधानी प्रारंभ में झील बालकश के दक्षिण में बलासाग़ून थी फिर काशग़र हुई और सामानी हुकूमत के अन्त के बाद 389 हि०/998 ई० में समरक़ंद बन गई। महमूद ग़ज़नवी ने समरक़न्द फ़तह करने के बाद ईलक ख़ानिया हुकूमत से सुलह कर ली थी कि जैहुन नदी दोनों सल्तन्तों के बीच सीमा निर्धारित होगी। बाद में उन हुक्मरानों ने सलजूक़ी और ख़्वारिज़्म शाही सल्तनत की आधारशिला स्वीकार कर ली थी। उस ज़माने के दस्तूर के अनुसार ये हुक्मरान जो मुसलमान थे ज्ञान एवं साहित्य के सरपरस्त भी थे। अतः प्रसिद्ध वैज्ञानिक हकीम उमर ख़ैयाम का प्रारंभिक संबंध इसी ख़ानदान के एक हुक्मरान शम्सुल मलिक (460 हि०/1067 ई० से 472 हि०/1079 ई०) के दरबार से था।] ने क़बज़ा करके सामानी हुकूमत का अन्त कर दिया।
बनू बुवैह (320 हि०/932 ई० से 447 हि०/1055 ई०)
सामानियों की तरह दूसरी बड़ी हुकूमत जो उस ज़माने में क़ायम हुई, वह 'बनू बुवैह' (Buwahid Dynasty) थी। इस ख़ानदान का 'वंश-प्रवर्त्तक' अबू शुजाअ बुवैह था। चूँकि इस ख़ानदान का सम्बन्ध 'माज़ंदरान' के इलाक़े 'देलम' से था, इसलिए बनू बुवैह को 'दयाल्मा' भी कहते हैं।
सामानियों की तरह यह भी एक ईरानी ख़ानदान था। इस हुकूमत के संस्थापक तीन भाई अली, हसन और अहमद थे, जिन्होंने क्रमशः इमादुद-दौला, रुकनुद-दौला और मअज़्ज़ुद-दौला की उपाधि ग्रहण की और ईरान एवं इराक़ में अलग-अलग हुकूमतें क़ायम कीं। इमादुद-दौला उनका मुख्य शासक था। उसके बाद यही हैसियत रुकनुद-दौला को प्राप्त हुई और उसके बाद मअज़्ज़ुद-दौला और उसकी औलादें इस ख़ानदान से मुख्य शासक बनीं। बग़दाद पर इस ख़ानदान के हुक्मरान मअज़्ज़ुद-दौला ने 334 हि०/945 ई० में क़बज़ा किया था। पूरा इराक़ और ख़ुरासान छोड़कर बाक़ी ईरान बनु बुवैह के क़बज़े में था। बग़दाद, असफ़हान और शीराज़ सल्तनत के बड़े शहर थे। सामानियों के पतन के बाद 'रै' पर भी उनका क़बज़ा हो गया।
बनू बुवैह का सबसे मशहूर हुक्मरान अज़ुदुद-दौला (366 हि०/976 ई० से 372 हि०/982 ई०) है। अज़ुदुद-दौला बादशाह बनने से पहले फ़ारस और करमान प्रांत का 28 साल तक वाली (गवर्नर) रहा। उसने पहले वाली की हैसियत से फिर बादशाह की हैसियत से जनकल्याण के बहुत-से काम किए और सल्तनत का बहुत विकास किया। उसने डाक-व्यवस्था इतनी सुचारु कर दी कि शीराज़ से क़ासिद (संदेशवाहक) सात दिन में बग़दाद पहुँच जाता था। हालाँकि दोनों शहरों के बीच लगभग छ: सौ मील की दूरी है। अरब और किरमान के रेगिस्तान उस ज़माने में डाकुओं का अड्डा बन गए थे, लेकिन अज़ुदुद-दौला ने वहाँ ऐसी शान्ति व्यवस्था की कि क़ाफ़िले बिना भय के सफ़र करने लगे।
अज़ुदुद-दौला ने बग़दाद का बहुत विकास किया। नहरें ख़ुदवाईं, दजला पर पुल बनवाया, शीराज़ में सिंचाई के लिए उसने एक बहुत बड़ा बाँध बनाया, जो ‘अमीर-बाँध' के नाम से अब तक मौजूद है। उसका एक और बड़ा कारनामा बग़दाद में एक विशाल अस्पताल स्थापित करना है। जनता के लिए अस्पताल खोलने की परम्परा हालाँकि उमवी ख़लीफ़ा वलीद के काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन अज़ुदुद-दौला का अस्पताल विशेष रूप से उल्लेखनीय था। यह अस्पताल दजला के किनारे एक विशाल भवन में था। यह इतना बड़ा था कि सारी दुनिया में कोई अस्पताल इसका मुक़ाबला नहीं कर सकता था। इसमें 24 चिकित्सक नियुक्त थे। जर्राह यानी ऑपरेशन करनेवाले, कहाल यानी आँखों का इलाज करनेवाले डाक्टर और मरहम-पट्टी करनेवाले कर्मचारी इसके अतिरिक्त थे।
इस अस्पताल के ख़र्च का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसके लिए साढ़े सात लाख रुपये सालाना की जागीर दे दी गई थी। यह अस्पताल (371 हि०/981 ई० से 656 हि०/1258 ई०) ढाई सौ साल से अधिक अर्से तक क़ायम रहा।
अज़ुदुद-दौला के बाद बनू बुवैह की हुकूमत में बिखराव प्रारंभ हो गया। इराक़, रै और फ़ारस में बुवैही ख़ानदान के शहज़ादों ने अलग-अलग हुकूमतें क़ायम कर लीं। उनमें रै की हुकूमत इस वजह से प्रसिद्ध थी कि उसके हुक्मरान फ़ख़रुद्दौला को एक बड़ा योग्य प्रधानमंत्री साहिब इब्ने अब्बाद मिल गया था। साहिब (373 हि०/983 ई० से 385 हि०/995 ई०) 12 वर्षों तक इस पद पर रहा और ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की जैसी अब्बासी ख़िलाफ़त के काल में बरामिका ने प्राप्त की थी। वह लेखक भी था, उसकी कई किताबें हैं। उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि एक बार एक सामानी बादशाह ने उसे प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा प्रकट की तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पुस्तकालय को स्थानांतरित करने के लिए चार सौ ऊँटों की ज़रूरत होगी।
रै की हुकूमत का 420 हि०/1029 ई० में ग़ज़नी के हुक्मरान महमूद ग़ज़नवी ने अन्त कर दिया। इसके बाद 447 हि०/1055 ई० में सलजूक़ियों ने बग़दाद पर क़बज़ा करके बनू बुवैह की सल्तनत का पूरी तरह अन्त कर दिया। बनू बुवैह शीया थे और मुहर्रम के अवसर पर ताज़िया निकालने एवं मुहर्रम की अन्य परम्पराओं का आग़ाज़ उन्हीं के हुक्मरान मुइज़्ज़ुद-दौला के काल से हुआ। बनू बुवैह ने अब्बासी ख़लीफ़ा को लाचार बना दिया और कई तरीक़ों से उसे अपमानित किया।
ज्ञान एवं साहित्य
बनू बुवैह के कई हुक्मरान और मंत्री ज्ञान एवं साहित्य के बड़े सरपरस्त थे। अज़ुदुद-दौला और साहिब इब्ने अब्बाद इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अरबी भाषा का सबसे बड़ा शायर मुतनब्बी (915 ई० से 965 ई०) इसी काल में हुआ है। उसने अज़ुदुद-दौला और साहिब की तारीफ़ में क़सीदे (महिमा काव्य) लिखे और पुरस्कार पाए।
प्रसिद्ध चिकित्सक और दार्शनिक बू अली सीना (370 हि०/980 ई० से 428 हि०/1036 ई०) इसी काल में हुआ है। 'राज़ी' के बाद इब्ने सीना सबसे बड़ा मुसलमान चिकित्सक हुआ है। चिकित्सा-शास्त्र पर उसने जो किताब लिखी उसका नाम 'शिफ़ा' है और दर्शन-शास्त्र पर जो सबसे बड़ी किताब लिखी उसका नाम 'क़ानून' है। ये दोनों किताबें कई-कई भागों में हैं और अरबी में हैं। बाद में उसकी किताबों का लातीनी और यूरोप की दूसरी ज़बानों में अनुवाद हुआ और फ़्रांस, जर्मनी तथा इटली के स्कूलों में कई सौ साल तक उसकी किताबें पढ़ाई जाती रहीं। उसने चिकित्सा विज्ञान में बहुत विस्तार किया। वह बहुत बड़ा दार्शनिक भी था।
उस काल के वैज्ञानिकों में इब्ने हैसम (354 हि०/965 ई० से 430 हि०/1039 ई०) का नाम भी उल्लेखनीय है। वह बसरा का रहनेवाला था और इब्ने सीना का समकालीन था। उसने जीव विज्ञान से सम्बन्धित कई किताबें लिखीं। यूरोप के अन्वेषकों का कहना है कि तस्वीर लेनेवाला कैमरा जिस सिद्धान्त की बुनियाद पर बनाया गया है वह सिद्धान्त सबसे पहले इब्ने हैसम ने ही पेश किया था। उसकी किताब 'किताबुल-मनाज़िर' जिसमें उसने यह सिद्धान्त पेश किया था बारहवीं सदी ई० में अरबी से लातीनी ज़बान में अनुवाद की गई और यूरोप के वैज्ञानिकों ने उससे फ़ायदा उठाया।
दर्शनशास्त्र की प्रसिद्ध किताब 'रसायल इख़्वानुस-सफ़ा' भी उसी काल में लिखी गई।
बनू बुवैह के इन कारनामों के बावजूद उनका शासनकाल मुसलमानों में अक़ीदे (आस्था) की कमज़ोरी और अख़लाक़ (चरित्र) की ख़राबी का कारण बना। अतः जब हम इस काल के पर्यटकों की किताबों को पढ़ते हैं तो इराक़ और ईरान के उन हिस्सों के बारे में जो बनू बुवैह के क़बज़े में थे, वैसी रौशन तस्वीर हमारे सामने नहीं आती जैसी सामानी शासनकाल में नज़र आती है। मुक़द्दसी इराक़ के बारे में लिखता है :
"इराक़ में गर्व किए जाने योग्य इतनी चीज़ें हैं कि गिनी नहीं जा सकतीं, परन्तु आजकल यह फ़ित्नों (अशांतियों) और महँगाई का घर बना हुआ है। दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। अत्याचार और अत्यधिक टैक्सों के कारण लोग मुसीबत में हैं और निर्लज्जता अधिक है।"
"बग़दाद लगभग उजड़ चुका है। मुझे आशंका है कि वह सामरा की तरह बरबाद हो जाएगा। फ़ित्ने, फ़साद (लड़ाई-झगड़े), अज्ञानता, दुराचार आदि का बाज़ार गर्म है और हुकूमत अत्याचारी है।"
"कूफ़ा एक समय में बग़दाद के समान था लेकिन इस समय स्थिति ख़राब है और बाहरी हिस्से उजड़े हुए हैं।"
बसरा की मुक़द्दसी ने प्रशंसा की है कि यह शहर उसे बग़दाद की अपेक्षा ज़्यादा पसन्द है क्योंकि आर्थिक सुविधाएँ ज़्यादा हैं और ज्ञान एवं कला विकास की ओर अग्रसर हैं।
धार्मिक भेदभाव और साम्प्रदायीकरण ने चौथी सदी हिजरी में मुसलमानों में मज़बूती से जड़ें पकड़ ली थीं और अब्बासी काल के ठीक विपरीत जहाँ विभिन्न अक़ीदे रखनेवाले आलिम मिल-जुलकर रहते थे, अब एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते नज़र आते हैं। बग़दाद साम्प्रदायकि दंगों का घर बन गया। इराक़ अजम के बारे में जहाँ हमदान का शहर स्थित है, मुक़द्दसी लिखता है कि नागरिक कट्टर हम्बली और अमीर मुआविया (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पक्के अनुयायी हैं और दूसरे मुसलमानों को काफ़िर क़रार देते हैं। इस सूबे में अक्सर दंगे होते रहते हैं।
असफ़हान और हमदान का उल्लेख करते हुए लिखता है—
"बनू बुवैह का संविधान निराला और रस्म-रिवाज बेहूदा है। बुवैह ख़ानदान के अत्याचारों से तंग आकर लोग देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आजकल उनकी हुकूमत अच्छी है। वह मुसलमानों की जायदाद को ज़ब्त नहीं करते और जब किसी को आर्थिक सहयोग देते हैं तो उसकी मौत तक जारी रखते हैं।"
ख़ूज़िस्तान के लोगों के बारे में लिखता है—
“यहाँ के लोगों को ज्ञान एवं साहित्य से दिलचस्पी नहीं और बच्चों को प्रारंभ से ही कारोबार में लगा देते हैं। व्यभिचार आम है।"
वह ख़ूज़िस्तान के पेट्रौल के कुओं का भी उल्लेख करता है।
शिराज़ जो बाद में ज्ञान एवं साहित्य का केन्द्र बना उसके सम्बन्ध में लिखता है—
"नागरिक हालाँकि सदाचारी हैं, परन्तु ज्ञान, साहित्य एवं शिष्टाचार में शून्य हैं।"
ख़ूज़िस्तान की तरह शीराज़ में भी वह व्यभिचार के आम होने की शिकायत करता है।
सीराफ़ की बंदरगाह अब्बासी काल में इतनी आबाद, इमारतें इतनी सुन्दर और बाज़ार इतने दर्शनीय थे कि लोग उसे बसरा से अच्छा समझते थे। लेकिन मुक़द्दसी लिखता है—
“बुवैही आधिपत्य के बाद आबादी कम हो गई और नागरिक शहर छोड़कर अम्मान के शहर 'सहार' में आबाद हो गए। 366 हि०/976 ई० के भूकम्प में शहर बिलकुल तबाह हो गया।"
मुक़द्दसी उस भूकम्प का उल्लेख करने के बाद लिखता है—
“मैंने नागरिकों से पूछा तुम्हारे चरित्र कैसे थे जो ख़ुदा ने तुमपर रहम न किया? बोले हमारे यहाँ बलात्कार, सूदख़ोरी बढ़ गई थी। मैंने कहा : इस तबाही से तुम लोगों ने इबरत (शिक्षा) ली? बोले, नहीं।”
मुक़द्दसी लिखता है कि अहले फ़ारस में अत्यधिक दुराचार के बावजूद सीराफ़ियों का व्यभिचार अपने चरम को पहुँचा हुआ था।
सल्तनते फ़ातिमिया (297 हि०/909 ई० से 567 हि०/1171 ई०)
इस काल की तीसरी बड़ी हुकूमत सल्तनते फ़ातिमिया है। यह हुकूमत 297 हि०/909 ई० में उत्तरी अफ़्रीक़ा के क़ैरवान शहर में स्थापित हुई। इस सल्तनत का संस्थापक उबैदुल्लाह चूँकि प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की औलाद में से था [कुछ इतिहासकारों को इस सम्बन्ध में मतभेद है।] इसलिए उसे 'सल्तनते फ़ातिमिया' कहा जाता है। उबैदुल्लाह इतिहास में मेहदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उबैदुल्लाह मेहदी और उसके अनुयायी शीया सम्प्रदाय की एक शाख़ हैं। ये लोग इमाम जाफ़र तक तो तमाम इमामों को मानते हैं, लेकिन इसके बाद वे इमाम जाफ़र के बड़े बेटे इसमाईल को इमाम मानते हैं, जबकि अस्ना-अशरी (शीया) मत के अनुसार इमामत का सिलसिला इमाम जाफ़र के दूसरे बेटे इमाम मूसा काज़िम की नस्ल में चलता है। फ़ातिमी ख़लीफ़ा चूँकि इसमाईल की औलाद में होने का दावा करते थे इसलिए वे 'इसमाईली' कहलाए। आग़ा ख़ानी ख़ूजे इसी इसमाईली सम्प्रदाय से संबंध रखते हैं।
अब तक जो हुकूमतें क़ायम हुई थीं वे हालाँकि आज़ाद हुकूमतें थीं, लेकिन सब बग़दाद की ख़िलाफ़त की अधीनता स्वीकार करती थीं और जुमा की नमाज़ के ख़ुत्बे में अब्बासी ख़लीफ़ा का नाम पढ़ती थीं, लेकिन फ़ातिमी हुक्मरानों ने अब्बासी ख़लीफ़ाओं का नाम ख़ुत्बा से निकाल दिया और ख़ुद ख़लीफ़ा होने का एलान किया, इसी लिए उनकी हुकूमत को 'ख़िलाफ़ते फ़ातिमिया' भी कहा जाता है।
प्रारंभ में फ़ातिमी हुकूमत उत्तरी अफ़्रीक़ा तक सीमित रही, लेकिन उनके हुक्मरान अल-मुइज़्ज़ (341 हि०/952 ई० से 365 हि०/975 ई०) ने 358 हि०/968 ई० में मिस्र भी फ़तह कर लिया। अल-मुइज़्ज़ फ़ातिमी हुकूमत का सबसे योग्य हुक्मरान है। वह अफ़्रीक़ा से मिस्र आ गया। मिस्र के वर्तमान नगर क़ाहिरा की बुनियाद उसी के काल में पड़ी। यह शहर फ़िसतात के निकट आबाद किया गया था और फ़ातिमियों की राजधानी था। उसके काल में 'जामे अज़हर' के नाम से क़ाहिरा में एक मसजिद का निर्माण किया गया। बाद में मसजिद में दीनी मदरसा [जामे अज़हर ने एक शैक्षणिक संस्थान की हैसियत 365 हि०/975 ई० में अज़ीज़ बिल्लाह के काल में प्राप्त की।] क़ायम किया गया। जामे अज़हर का यह मदरसा दुनिया का सबसे पुराना मदरसा है जो अब तक मौजूद है और दुनिया के हर हिस्से से मुसलमान छात्र वहाँ मज़हबी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।
अल-मुइज़्ज़ के बाद उसका लड़का अज़ीज़ (365 हि०/975 ई० से 386 हि०/996 ई०) तख़्त पर बैठा। वह भी एक योग्य शासक था। उसके काल में शाम (सीरिया), हिजाज़, यमन पर भी फ़ातिमियों का क़बज़ा हो गया और इस प्रकार फ़ातिमी हुकूमत इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई।
फ़ातिमियों के काल में मुसलमानों की समुद्री ताक़त का बहुत विकास हुआ। सक़लिया और इटली का दक्षिणी भाग उनके क़बज़े में था। फ़ातिमी बेड़े जेनेवा, रूम और नेपल्ज़ पर हमले करते रहते थे और यूरोप के समुद्री बेड़े उनके मुक़ाबले में ठहर नहीं सकते थे।
अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन के बाद इस समय तक जो हुकूमतें क़ायम हुईं उनमें फ़ातिमी सल्तनत न केवल सबसे बड़ी और शक्तिशाली थी बल्कि सबसे अधिक स्थिर और विशाल थी। यह हुकूमत 297 हि०/909 ई० से 567 हि०/1171 ई० तक (लगभग पौने तीन सौ साल तक) क़ायम रही। 567 हि० में शाम (सीरिया) के हुक्मरान नूरुद्दीन ने इस हुकूमत का अंत कर दिया जिसके बाद मिस्र में अब्बासी ख़लीफ़ा का नाम ख़ुत्बा में लिया जाने लगा।
फ़ातिमियों के काल में ज्ञान एवं साहित्य की सामानियों या बनू बुवैह की तरह तरक़्क़ी नहीं हुई, हाँ, उन्होंने शहर क़ाहिरा को बहुत तरक़्क़ी दी। अच्छी-अच्छी इमारतें बनवाईं। अपने महलों को सुन्दर से सुन्दर सामान और कपड़ों से सजाया। कपड़े और शीशा बनाने के काम ने उस काल में बड़ी तरक़्क़ी की। उनके काल की कई यादगारें क़ाहिरा में देखी जा सकती हैं। लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि 'जामे अज़हर' को प्राप्त है।
नासिर ख़ुसरो (394 हि०/1003 ई० से 452 हि०/1060 ई०)
फ़ातिमियों के काल में ख़ुरासान का एक बहुत बड़ा लेखक और पर्यटक नासिर ख़ुसरो (394 हि०/1003 ई० से 452 हि०/1060 ई०) मिस्र आया था। उसने अपने यात्रा-वृतांत में मिस्र और शाम की बड़ी रोचक घटनाएँ लिखी हैं। यह काल चूँकि फ़ातिमियों के पतन का था, लेकिन फिर भी इस यात्रा-वृतांत से अंदाज़ा होता है कि ये दोनों क्षेत्र उस काल में कितने विकसित थे। वह लेबनान के शहर 'तराबुलस-अश-शाम' के सम्बन्ध में लिखता है कि यहाँ के मकान चार और छः मंज़िल के हैं, गलियाँ और बाज़ार मुहल्लों की तरह साफ़-सुथरे हैं। यहाँ समरक़ंद से अच्छा काग़ज़ बनता है। बीस हज़ार आबादी है।
सीदा (Sidon) के सम्बन्ध में लिखता है—
“यहाँ का बाज़ार ऐसा सजा हुआ था कि मैंने इसे देखकर समझा कि बादशाह के स्वागत के लिए सजाया गया है। बाद में मालूम हुआ कि यह शहर हमेशा ऐसा ही सजा हुआ रहता है।"
सूर (Tyre), रमला और तनिस (Tenes) के सम्बन्ध में लिखता है—
“शहर सूर में पाँच या छः मंज़िल की इमारतें हैं, फ़व्वारे बहुत अधिक हैं, बाज़ार ख़ूबसूरत सामानों से पटे पड़े हैं। शाम के शहरों में सम्पन्नता के लिहाज़ से ये शहर मिसाल देने लायक़ है। रमला में अक्सर इमारतें संगमरमर की हैं, जिनपर नक़्क़ाशी की गई है। यहाँ से अच्छा इंजीनियर कहीं नहीं होता।”
"तनिस (Tenes) के शहर में दो सौ दुकानें केवल इत्रवालों की हैं। यहाँ एक ख़ास क़िस्म का रेश्मी और सूती कपड़ा बनाया जाता है, जो दूसरी जगह नहीं बनाया जाता। घाट पर एक हज़ार कश्तियाँ रहती हैं।"
वर्तमान काल से पहले ऊँची इमारतें बनाने का ज़्यादा रिवाज नहीं था, लेकिन क़ाहिरा की इमारतों का नासिर ख़ुसरो ने जो हाल लिखा है उससे मालूम होता है कि गगनचुम्बी इमारतों के लिहाज़ से क़ाहिरा को दुनिया में वही हैसियत हासिल थी जो आजकल न्यूयार्क और दूसरे अमेरिकी शहरों को हासिल है। वह लिखता है कि क़ाहिरा की अक्सर इमारतें पाँच और छ: मंज़िल की हैं और फ़िसतात (क़ाहिरा का पुराना भाग) की कुछ इमारतें सात से चौदह मंज़िल तक की हैं। मकानों के अन्दर बाग़ और चमन हैं और लोग छतों पर भी सैरगाहें बनाते हैं। मकान पाकीज़गी और सुन्दरता में अद्भुत हैं। शहर में कम से कम बीस हज़ार दुकानें हैं और पचास हज़ार ऊँट पानी भरते हैं। क़ंदीलों का बाज़ार सबसे अच्छा है। कुछ बाज़ारों में दिन-रात क़ंदीलें रौशन रहती हैं। शहर में दो सौ सराय हैं। सबसे बड़ी सराय का किराया बीस हज़ार दीनार सालाना वसूल होता है।
उद्योग के सम्बन्ध में लिखता है कि मिट्टी के बरतन ऐसे पारदर्शी बनते हैं कि हाथ रखो तो दूसरी तरफ़ दिखाई देता है। इसी प्रकार शीशा भी साफ़ बनता है।
दौलते सामानिया
(261 हि०/874 ई० से 395 हि०/1005 ई०)
1. नसर अव्वल - 261 हि०/874 ई० से 279 हि०/892 ई०
2. इसमाईल - 279 हि०/892 ई० से 295 हि० 907 ई०
3. अहमद - 295 हि०/907 ई० से 301 हि०/913 ई०
4. नसर द्वितीय - 301 हि०/913 ई० से 331 हि०/942 ई०
5. नूह अव्वल - 331 हि०/942 ई० से 343 हि०/954 ई०
6. अब्दुल मलिक - 343 हि०/954 ई० से 350 हि०/961 ई०
7. मंसूर अव्वल - 350 हि०/961 ई० से 366 हि०/976 ई०
8. नूह द्वितीय - 366 हि०/976 ई० से 387 हि०/997 ई०
9. मंसूर द्वितीय - 387 हि०/997 ई० से 389 हि०/999 ई०
10. अब्दुल मलिक - 389 हि०/999 ई० से 395 हि०/1005 ई०
बनू बुवैह
(320 हि०/932 ई० से 447 हि०/1055 ई०)
1. इमादुद्दौला - 320 हि०/932 ई० से 338 हि०/949 ई०
2. रुकनुद्दौला - 338 हि०/949 ई० से 366 हि०/977 ई०
3. अज़ुदुद्दौला - 366 हि०/977 ई० से 372 हि०/983 ई०
4. समसामुद्दौला - 372 हि०/983 ई० से 376 हि०/986 ई०
5. शर्फ़ुद्दौला - 376 हि०/986 ई० से 379 हि०/989 ई०
6. बहाउद्दौला - 379 हि०/989 ई० से 402 हि०/1011 ई०
7. सुल्तानुद्दौला - 402 हि०/1011 ई० से 411 हि०/1020 ई०
8. शर्फ़ुद्दौला द्विर्तीय - 411 हि०/1020 ई० से 416 हि०/1025 ई०
9. जलालुद्दौला - 416 हि०/1025 ई० से 435 हि०/1043 ई०
10. अबू कालीजार - 435 हि०/1043 ई० से 440 हि०/1048 ई०
11. मलिक रहीम - 440 हि०/1048 ई० से 447 हि०/1054 ई०
ख़िलाफ़ते फ़ातिमिया
(297 हि०/909 ई० से 567 हि०/1171 ई०)
1. मेहदी - 297 हि०/909 ई० से 322 हि०/934 ई०
2. क़ायम - 322 हि०/934 ई० से 334 हि०/945 ई०
3. मंसूर - 334 हि०/945 ई० से 341 हि०/952 ई०
4. मुइज़्ज़ - 341 हि०/952 ई० से 365 हि०/975 ई०
5. अज़ीज़ - 365 हि०/975 ई० से 386 हि०/996 ई०
6. हाकिम - 386 हि०/996 ई० से 411 हि०/1020 ई०
7. ज़ाहिर - 411 हि०/1020 ई० से 427 हि०/1035 ई०
8. मुसतंसर - 427 हि०/1035 ई० से 487 हि०/1094 ई०
9. मुसताली - 487 हि०/1094 ई० से 495 हि०/1101 ई०
10. आमिर - 495 हि०/1101 ई० से 524 हि०/1130 ई०
11. हाफ़िज़ - 524 हि०/1130 ई० से 544 हि०/1149 ई०
12. जाफ़िर - 544 हि०/1149 ई० से 549 हि०/1154 ई०
13. फ़ाइज़ - 549 हि०/1154 ई० से 555 हि०/1160 ई०
14. आज़िद - 555 हि०/1160 ई० से 567 हि०/1171 ई०
अध्याय-14
ग़ज़नी की सल्तनत
हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत का प्रारंभ बनी उमय्या के काल ही में हो गया था, जबकि मुहम्मद बिन क़ासिम ने मकरान, सिंध और मुल्तान को जीतकर उन इलाक़ों को इस्लामी ख़िलाफ़त में शामिल कर लिया था। ख़िलाफ़ते बग़दाद के पतन तक ये इलाक़े इस्लामी ख़िलाफ़त में शामिल रहे, परन्तु उनकी हैसियत सरहदी प्रान्तों की थी। अरबों के काल में मुसलमानों ने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की।
पाकिस्तान और भारत में इस्लामी विजयों का दूसरा दौर मुहम्मद बिन क़ासिम के तीन सौ साल बाद शुरू हुआ। इस बार मुसलमान मकरान के रास्ते से नहीं बल्कि ख़ैबर दर्रे के रास्ते आए। इसका विवरण इस प्रकार है—
जब सामानी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उसके सूबेदार स्वतन्त्र हो गए। उनमें एक सूबेदार सुबक्तगीन (366 हि०/976 ई० से 387 हि०/997 ई०) ने ग़ज़नी में, जो अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में एक शहर है, 366 हि०/976 ई० में एक आज़ाद हुकूमत क़ायम कर ली थी, जो इतिहास में दौलते ग़ज़नविया और आले सुबक्तगीन के नाम से जानी जाती है। बाद में ख़ुरासान पर भी सुबक्तगीन के काल में मुसलमान पहली बार ख़ैबर दर्रे के रास्ते पाकिस्तान में दाख़िल हुए।
उस काल में लाहौर में एक हिन्दू राजा हुकूमत करता था, जिसका नाम जयपाल था। उसकी हुकूमत पेशावर से आगे काबुल तक फैली हुई थी और उसकी सीमाएँ सुबक्तगीन की हुकूमत से मिली हुई थीं। राजा जयपाल ने जब देखा कि सुबक्तगीन की हुकूमत शक्तिशाली बन रही है तो उसने एक बड़ी फ़ौज लेकर ग़ज़नी की हुकूमत पर हमला कर दिया। लेकिन लड़ाई में सुबक्तगीन ने जयपाल को पराजित कर दिया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। जयपाल ने सुबक्तगीन की अधीनता स्वीकार करके अपनी जान बचाई और वार्षिक ख़िराज देने का वादा किया। अब सुबक्तगीन ने जयपाल को रिहा कर दिया और वह लाहौर वापस आ गया परन्तु उसने अपने वादे के अनुसार ख़िराज नहीं भेजा, जिसके कारण सुबक्तगीन ने हमला कर दिया और पेशावर घाटी पर क़बज़ा कर लिया।
महमूद ग़ज़नवी (387 हि०/997 ई० से 421 हि०/1030 ई०)
बीस साल की हुकूमत के बाद सुबक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का महमूद ग़ज़नवी गद्दी पर बैठा। महमूद सुबक्तगीन ख़ानदान का सबसे बड़ा बादशाह हुआ है। वह इस्लामी इतिहास के प्रसिद्ध शासकों में गिना जाता है। महमूद बचपन ही से बड़ा निडर और बहादुर था। वह अपने बाप के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका था। बादशाह होने के बाद उसने अपनी सल्तनत का बहुत विस्तार किया। महमूद बड़ा सफल सिपहसालार और एक बड़ा विजेता था। उत्तर में उसने ख़्वारिज़्म और बुख़ारा पर क़बज़ा कर लिया और समरक़ंद के इलाक़े के छोटे-छोटे हुक्मरानों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे पहले बुख़ारा और समरक़ंद, काशग़र के ईलक ख़ानिया हुक्मरानों के क़बज़े में थे और ख़्वारिज़्म में एक छोटी-सी स्वतन्त्र हुकूमत आले मामून के नाम से क़ायम थी। दक्षिण में उसने रै, अस्फ़हान और हमदान जीत लिए जो बनू बुवैह के क़बज़े में थे। पूरब में उसने लगभग वे तमाम इलाक़े अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए जो अब पाकिस्तान कहलाते हैं।
ऊपर बताया जा चुका है कि लाहौर की हुकूमत पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, परन्तु वहाँ के राजा बार-बार ख़िराज की रक़म बंद कर देते थे और भारत के राजाओं से मदद लेकर महमूद के मुक़ाबले पर आ जाते थे। महमूद ने उन्हें कई बार पराजित किया और आख़िर तंग आकर 412 हि०/1021 ई० में लाहौर की हुकूमत को सीधे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। महमूद ने उन राजाओं के इलाक़ों पर भी हमला किया जो लाहौर के राजा की मदद किया करते थे। और इस प्रकार उसने क़न्नौज और कालिंजर तक अपनी सल्तनत बढ़ा दी, परन्तु इन इलाक़ों पर महमूद ने अपनी प्रत्यक्ष हुकूमत क़ायम नहीं की, बल्कि राजाओं से अधीनता का वादा लेकर ग़ज़नी वापस चला गया। महमूद का आख़िरी हमला सोमनाथ पर हुआ। सोमनाथ से वापसी पर महमूद ने मंसूरा जीतकर सिंध को भी अपनी सल्तनत में मिला लिया। पाकिस्तान और भारत पर महमूद ने कुल सतरह हमले किए। उन हमलों के कारण उसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, परन्तु सच्ची बात यह है कि इन हमलों से इस्लाम को कोई लाभ नहीं पहुँचा। महमूद की फ़ौजें दिल्ली, मथुरा, क़न्नौज, कालिंजर और सोमनाथ तक पहुँच गईं लेकिन वे लड़ाई लड़कर, माले ग़नीमत लूटकर एवं अधीनता का वादा लेकर वापस चली जाती थीं। ये राजा बार-बार बाग़ी हो जाते थे और महमूद को पुनः वापस आना पड़ता था। महमूद के ये हमले ख़िलाफ़ते राशिदा और बनी उमय्या की जीतों से पूर्णतः भिन्न थे। उनके काल में जो देश जीते गए उनपर मुसलमानों ने बाक़ायदा हुकूमत क़ायम कर दी थी और एक व्यवस्था स्थापित कर दी थी जो पहले से अच्छी थी, लेकिन महमूद ने पंजाब के अतिरिक्त और किसी इलाक़े को अपनी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया। इसके कारण महमूद को बार-बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। रुपये बरबाद हुए, लोगों की जानें बरबाद हुईं और हिन्दू यह समझने लगे कि मुसलमान केवल लड़ाकू और लुटेरे हैं। यह राय ईरानी और रूमी नागरिक अरबों के सम्बन्ध में नहीं क़ायम कर सकते थे, क्योंकि अरबों ने जो भी इलाक़ा जीता वहाँ मज़बूत हुकूमत क़ायम की।
महमूद ग़ज़नवी का न्याय
महमूद एक बड़ा विजेता एवं सिपहसालर होने के अलावा प्रजा की देखभाल करनेवाला भी था। उसके न्याय एवं इनसाफ़ के बहुत-से क़िस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार एक व्यापारी ने सुल्तान महमूद से उसके लड़के शहज़ादा मसऊद की शिकायत की और कहा कि मैं परदेसी व्यापारी हूँ और बहुत दिनों से इस शहर में पड़ा हुआ हूँ। घर जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि शहज़ादा ने मुझसे साठ हज़ार दीनार का सौदा ख़रीदा है और क़ीमत अदा नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि शहज़ादा मसऊद को क़ाज़ी (न्यायाधीश) के सामने भेजा जाए। महमूद को व्यापारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मसऊद को सूचित करवाया कि या तो व्यापारी को क़ीमत अदा कर दे या कचहरी में क़ाज़ी के सामने हाज़िर हो, ताकि शरई आदेश जारी किया जाए। जब सुल्तान का संदेश मसऊद तक पहुँचा तो उसने तुरंत अपने ख़ज़ांची से पूछा कि ख़ज़ाने में कितनी नक़द रक़म मौजूद है। उसने बताया, बीस हज़ार दीनार। शहज़ादे ने कहा, ये रक़म व्यापारी को देकर शेष के लिए तीन दिन का समय माँग लो। ख़ज़ांची ने उसके आदेश का पालन किया। उधर शहज़ादे ने सुल्तान को सूचित करवा दिया कि मैंने बीस हज़ार दीनार अदा कर दिए हैं और तीन दिन में शेष रक़म भी अदा कर दूँगा। सुल्तान ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता जब तक तुम व्यापारी की रक़म नहीं अदा करोगे, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। मसऊद को जब यह जवाब मिला तो उसने इधर-उधर से क़र्ज़ लेकर दूसरी नमाज़ के वक़्त तक साठ हज़ार दीनार व्यापारी को अदा कर दिए। इसी प्रकार एक बार ईरान के किसी इलाक़े में जिसे हाल ही में महमूद ने जीता था, व्यापारियों का एक क़ाफ़िला लुट गया। उस क़ाफ़िले में एक बुढ़िया का लड़का भी था। बुढ़िया ने जब महमूद से इसकी शिकायत की तो उसने कहा कि वह इलाक़ा बहुत दूर है, इसलिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठिन है। बुढ़िया भी साहसी थी, उसने जवाब दिया कि जब तुम किसी इलाक़े की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते तो नए-नए देश क्यों जीतते हो। महमूद ने जब बुढ़िया का यह जवाब सुना तो वह बहुत लज्जित हुआ। बुढ़िया को तो रुपये-पैसे देकर विदा कर दिया, परन्तु उस इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दी कि व्यापारियों के क़ाफ़ले को लूटने की हिम्मत फिर किसी ने नहीं की।
ज्ञान एवं साहित्य
महमूद ग़ज़नवी ज्ञान एवं साहित्य का संरक्षक एवं प्रेमी था। अब्बासी ख़लीफ़ाओं के बाद इतिहास में दो-चार ही बादशाह मिलेंगे जो महमूद की तरह ज्ञान एवं कला के संरक्षक रहे हों। ज्ञान एवं कला के प्रति उसके इस आदर भाव के कारण उसके दरबार में बड़े-बड़े योग्य व्यक्ति जमा हो गए। उनमें केवल कवियों की संख्या चार सौ थी। उन कवियों में सबसे प्रसिद्ध फ़िरदौसी हैं।
फ़िरदौसी ने 'शाहनामा' के नाम से एक किताब लिखी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शाहनामा में न तो महमूद की विजय-गाथा है न तो मुसलमानों के शानदार कारनामों का उल्लेख। इसमें तो इस्लाम से पहले के ईरानी बादशाहों के झूठे-सच्चे हालात बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं। परन्तु इतनी ख़ूबी से लिखे गए हैं कि यह शाहनामा फ़ारसी पद्य का उत्कृष्ट नमूना समझा जाता है और दुनिया इसे आज तक दिलचस्पी से पढ़ती है।
महमूद ने फ़ारसी भाषा का सामानियों से भी अधिक संरक्षण किया, जिसके कारण अब फ़ारसी भाषा भी विकासशील हो गई।
महमूद के काल का एक बहुत बड़ा अन्वेषक अल-बैरूनी (362 हि०/972 ई० से 440 हि०/1048 ई०) था। अल-बैरूनी अपने काल का सबसे बड़ा अन्वेषक और वैज्ञानिक था। उसने गणित, खगोल शास्त्र, इतिहास एवं भूगोल में ऐसी-ऐसी श्रेष्ठ किताबें लिखीं जो अब तक शौक़ से पढ़ी जाती हैं। उनमें एक किताब 'अलहिन्द' है। इसमें उसने हिन्दुओं की धार्मिक आस्थाओं, उनके इतिहास और पाकिस्तान एवं भारत के भौगोलिक हालात बहुत खोजपूर्ण रूप से लिखे हैं। इस किताब से हिन्दुओं के इतिहास से सम्बन्धित जो जानकारी प्राप्त होती है, उनमें से बहुत-सी जानकारी ऐसी है जो और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। इस किताब को लिखने में उसने बहुत मेहनत की। हिन्दू ब्राह्मण अपना ज्ञान किसी दूसरे को सिखाते नहीं थे, परन्तु अल-बैरूनी ने कई साल पश्चिमी पाकिस्तान में रहकर संस्कृत भाषा सीखी और हिन्दुओं के ज्ञान में ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली कि ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे। अल-बैरूनी की एक प्रसिद्ध किताब 'क़ानूने मसऊदी' है, जो उसने महमूद के लड़के सुल्तान मसऊद के नाम पर लिखी। यह अंतरिक्ष विज्ञान एवं गणित की बड़ी अहम किताब है। इसके कारण अल-बैरूनी को एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ समझा जाता है।
महमूद ने ग़ज़नी शहर को भी बहुत विकसित किया। जब वह बादशाह बना तो यह एक मामूली शहर था, लेकिन महमूद ने अपने तीस साल की हुकूमत में ग़ज़नी को दुनिया का एक विशाल और विकसित शहर बना दिया। यहाँ उसने एक विशाल मसजिद का निर्माण करवाया, एक बहुत बड़ा मदरसा और एक संग्रहालय भी बनाया। उसने क़न्नौज की विजय की यादगार के लिए एक मीनार भी बनाया जो अब तक ग़ज़नी में मौजूद है।
महमूद ग़ज़नवी के बाद ग़ज़नी की सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। महमूद के लड़के मसऊद के अन्तिम काल में सलजूक़ी तुर्कों ने, जो मध्य एशिया से आए थे, ग़ज़नवी सल्तनत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर क़बज़ा कर लिया। अब ग़ज़नवी सल्तनत के क़बज़ा में केवल वे इलाक़े रह गए जो अब पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान कहलाते हैं।
पतनकाल के ग़ज़नवी हुक्मरानों में सुल्तान इबराहीम (451 हि०/1059 ई० से 492 हि०/1099 ई०) का नाम सबसे प्रसिद्ध है। उसने अपने चालीस वर्षीय शासनकाल में सल्तनत को बहुत सुदृढ़ बनाया। सलजूक़ियों से अच्छे सम्बन्ध बनाए और भारत में कई युद्धों में विजयी भी हुआ। उसके काल में हिन्दुओं ने मुसलमानों को पंजाब से बेदख़ल करने की कोशिश की, परन्तु वे इसमें सफल नहीं हुए। इबराहीम ने दिल्ली तक तमाम इलाक़ा ग़ज़नी की सल्तनत में सम्मिलित कर लिया और उसकी फ़ौजों ने वाराणसी तक सफ़ल आक्रमण किए।
इबराहीम बड़ा धर्मपरायण और प्रजा का ध्यान रखनेवाला शासक था। रात को ग़ज़नी के मुहल्लों में गश्त करता और ज़रूरतमंदों एवं विधवाओं को तलाश करके उनकी मदद करता था। वह एक श्रेष्ठ कातिब था। हर वर्ष एक क़ुरआन लिखता, जिसे एक साल मक्का और दूसरे साल मदीना भेज देता था। उसे महल बनाने से ज़्यादा शौक़ ऐसी इमारतों को बनाने का था, जिनसे लोग लाभ उठा सकें। अत: उसके काल में चार सौ से अधिक मदरसे, ख़ानक़ाहें, मुसाफ़िरख़ाने और मसजिदें बनाईं गईं। उसने ग़ज़नी के शाही महल में एक बहुत बड़ा दवाख़ाना क़ायम किया था, जहाँ लोगों को मुफ़्त दवाएँ मिलती थीं। इस दवाख़ाने में विशेष रूप से आँख की बीमारियों की बड़ी अच्छी दवाएँ थीं।
545 हि०/1150 ई० में ग़ज़नी पर इलाक़ा ग़ौर के एक हुक्मरान अलाउद्दीन ने क़बज़ा करके शहर में आग लगा दी, जिसके कारण दुनिया का यह महान शहर जलकर ख़ाक हो गया। अलाउद्दीन के इस ज़ालिमाना काम से लोग उसे 'जहाँसोज़' यानी दुनिया का जलानेवाला कहते हैं। उसके बाद ग़ज़नवी ख़ानदान के अन्तिम दो हुक्मरानों की राजधानी लाहौर हो गई। 582 हि०/1186 ई० में ग़ौर के एक दूसरे हुक्मरान शहाबुद्दीन ने लाहौर पर क़बज़ा करके 'आले सुबक्तगीन' की हुकूमत का अन्त कर दिया।
ग़ज़नवी हुक्मरानों का काल पाकिस्तान के इतिहास में विशेषकर बहुत महत्त्व रखता है। पश्चिमी पाकिस्तान लगभग दो सौ साल तक ग़ज़नी की सल्तनत का एक हिस्सा रहा और इस काल में इस क्षेत्र में इस्लामी सभ्यता की जड़ें मज़बूत हुईं। कोहे सुलैमान के इलाक़े में रहनेवाले पठानों ने इसी काल में इस्लाम धर्म स्वीकार किया और लाहौर पहली बार ज्ञान एवं साहित्य का केन्द्र बना। उसी काल में फ़ारसी के कई साहित्यकार एवं कवि या तो लाहौर में पैदा हुए या यहाँ आकर आबाद हो गए। यहाँ के कवियों में मसऊद, सअद सलमान और रूनी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये फ़ारसी के अग्रणी कवियों में गिने जाते हैं। ये दोनों कवि सुल्तान इबराहीम और उसके उत्तराधिकारियों के काल में थे।
लाहौर के आलिमों में हज़रत अली बिन उसमान हुजवेरी (400 हि०/1010 ई० से 465 हि०/1072 ई०) बहुत प्रसिद्ध हैं। वे एक बहुत बड़े वली हुए हैं। उनकी कोशिशों से लाहौर के इलाक़े में इस्लाम का प्रसार हुआ और बहुत-से लोग मुसलमान हुए। हज़रत हुजवेरी (रहमतुल्लाह अलैह) आजकल 'दातागंज बख़्श' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े भाग की चालीस वर्ष तक सैर की और अन्त में लाहौर आकर रहने लगे। उनकी क़ब्र अब तक लाहौर में मौजूद है।
हज़रत हुजवेरी (रहमतुल्लाह अलैह) 'कशफ़ुल-महजूब' नामक एक पुस्तक के लेखक हैं। यह इल्मे तसव्वुफ़ में फ़ारसी भाषा की पहली किताब है और तसव्वुफ़ की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। यह किताब उन्होंने लाहौर में लिखी। इस किताब का उर्दू और हिन्दी में भी अनुवाद हो गया है।
ग़ज़नवी काल की चर्चा समाप्त करने से पूर्व इस काल की दो महान हस्तियों की चर्चा करना ज़रूरी है। इनमें एक अबू सईद अबुल-ख़ैर (357 हि०/967 ई० से 440 हि०/1049 ई०) हैं, जो अपने काल के बड़े सूफ़ी और वली थे। उनकी प्रसिद्धि अधिकतर रुबाइयों (उर्दू-फ़ारसी पद्य की एक विधा) के कारण है, क्योंकि वह इस विधा में फ़ारसी भाषा के पहले बड़े कवि हैं। उनकी रुबाइयाँ आज भी लोकप्रिय हैं और अल्लाह से मुहब्बत एवं नैतिकता उनका प्रमुख विषय है।
दूसरी हस्ती, सनाई (465 हि०/1072 ई० से 545 हि०/1150 ई०) की है। सनाई ग़ज़नवियों के अन्तिम दौर के सबसे बड़े कवि हैं और फ़ारसी में सूफ़ी कविता के प्रवर्तक हैं। उनकी कविता नैतिक शिक्षाओं से भरी हुई है। अबू सईद अबुल-ख़ैर का सम्बन्ध ख़ुरासान से था और सनाई का ग़ज़नी से।
अरबी भाषा का प्रसिद्ध साहित्यकार बदीउज़्ज़मा हमदानी (मृत्यु-398 हि०/1007 ई०) भी इसी काल से सम्बन्ध रखता है। वह हरात का रहनेवाला था। उसकी किताब 'मक़ामात' अरबी साहित्य का उत्कृष्ट नमूना समझी जाती है।
ग़ज़नवी सल्तनत
(366 हि०/976 ई० से 582 हि०/1186 ई०)
1. सुबक्तगीन - 366 हि०/976 ई० से 387 हि०/997 ई०
2. महमूद - 387 हि०/997 ई० से 421 हि०/1030 ई०
3. मसऊद प्रथम - 421 हि०/1030 ई० से 432 हि०/1040 ई०
4. मौदूद - 432 हि०/1040 ई० से 440 हि०/1048 ई०
5. अब्दुर्रशीद - 440 हि०/1048 ई० से 444 हि०/1052 ई०
6. फ़र्रुख़ज़ाद - 444 हि०/1052 ई० से 451 हि०/1059 ई०
7. इबराहीम - 451 हि०/1059 ई० से 492 हि०/1099 ई०
8. मसऊद द्वितीय - 492 हि०/1099 ई० से 508 हि०/1114 ई०
9. शहज़ाद - 508 हि०/1114 ई० से 509 हि०/1115 ई०
10. अर्सलान शाह - 509 हि०/1115 ई० से 512 हि०/1118 ई०
11. बहराम शाह - 512 हि०/1118 ई० से 547 हि०/1152 ई०
12. ख़ुसरू शाह - 547 हि०/1152 ई० से 555 हि०/1160 ई०
13. ख़ुसरू मलिक - 555 हि०/1160 ई० से 582 हि०/1186 ई०
-------------
मुल्तान की जीत - 396 हि०/1005 ई०
पेशावर की जंग, आनंद पाल की पराजय - 399 हि०/1008 ई०
क़न्नौज के राजा की अधीनता - 408 हि०/1017 ई०
कालिंजर के राजा की अधीनता - 413 हि०/1022 ई०
सोमनाथ पर हमला - 415 हि०/1024 ई०
अध्याय-15
सलजूक़ी तुर्क
अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन के बाद इस्लामी दुनिया दो सौ साल तक छोटी-छोटी हुकूमतों में बँटी रही जैसाकि पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है। लेकिन इसके बाद सलजूक़ी तुर्कों ने इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से को एक बार फिर संगठित किया। ये सलजूक़ी 'तुर्क' नस्ल के थे और इस्लाम क़बूल करने के बाद मध्य एशिया के मैदानों से निकलकर ख़ुरासान में आबाद हो गए थे। जिस काल में ये ख़ुरासान में आबाद हुए वहाँ ग़ज़नवी सल्तनत क़ायम थी।
जब इस हुकूमत का पतन प्रारंभ हुआ तो ग़ज़नवी हुक्मरानों से सलजूक़ियों की ख़ुरासान में बहुत लड़ाइयाँ हुईं। सलजूक़ी सरदार का नाम तुग़रिल (429 हि०/1037 ई० से 455 हि०/1063 ई०) था। तुग़रिल बड़ा योग्य सिपहसालार था। उसने (429 हि०/1037 ई०) में दिनदानीक़ान की जंग में ग़ज़नवी हुक्मरान मसऊद को पराजित करके ख़ुरासान में सलजूक़ी हुकूमत की बुनियाद डाल दी। ख़ुरासान में हुकूमत मज़बूत हो जाने के बाद तुग़रिल ने पश्चिम का रुख़ किया और ईरान पर विजय प्राप्त करता हुआ 447 हि०/1055 ई० में बग़दाद में दाख़िल हो गया जो बनू बुवैह के क़बज़े में था।
तुग़रिल इतिहास के बड़े योद्धाओं एवं सिपहसालारों में गिना जाता है। उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी सल्तनत क़ायम कर दी जो सामानियों, बनू बुवैह और बनी फ़ातिमा सबकी हुकूमतों से बड़ी थी। उसने इस विशाल सल्तनत पर 26 साल तक बड़ी दक्षता से हुकूमत की।
अल्प अर्सलान (455 हि०/1063 ई० से 465 हि०/1072 ई०)
तुग़रिल के बाद उसका भतीजा अल्प अर्सलान गद्दी पर बैठा। अल्प अर्सलान ने आरमीनिया, एशिया-ए-कोचक, उत्तरी शाम (सीरिया) और मावराउन-नहर को जीत करके सलजूक़ियों की सल्तनत को और विस्तृत कर दिया। उसके नाम का ख़ुत्बा मक्का और मदीना में भी पढ़ा जाने लगा जो उससे पहले फ़ातमियों के क़बज़े में थे। अल्प अर्सलान ने एशिया-ए-कोचक के शहर 'मलाज़गिर्द' के पास रूमी बादशाह को 1071 ई० में ज़बर्दस्त शिकस्त दी, जिसके कारण उसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
हम यह पढ़ चुके हैं कि अरबों के काल में एशिया-ए-कोचक पूरी तरह फ़तह नहीं हुआ था। आधे मुल्क पर मुसलमान क़ाबिज़ थे और आधा रूमियों के क़बज़े में था, जिनकी राजधानी क़ुस्तनतीनिया थी। जब अब्बासी सल्तनत का पतन हुआ तो एशिया-ए-कोचक में रूमियों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने पूरा इलाक़ा मुसलमानों से छीन लिया। रूमियों ने जब यह देखा कि सलजूक़ियों ने एक बड़ी सल्तनत क़ायम कर ली है जो रूमी सल्तनत के लिए ख़तरा हो सकती है तो रूमी बादशाह अरमानूस दो लाख फ़ौज लेकर अल्प अर्सलान से लड़ने के लिए चला। अल्प अर्सलान के पास केवल पंद्रह हज़ार फ़ौज थी और वह मुक़ाबला के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने सबसे पहले सुलह की कोशिश की परन्तु अरमानूस ने जवाब दिया कि सुलह तुम्हारी राजधानी 'रै' में पहुँचकर होगी। रूमी बादशाह के इस जवाब के बाद अल्प अर्सलान भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। जुमा (शुक्रवार) का दिन था। सुल्तान ने पहले नमाज़ पढ़ी और ख़ुदा से फ़तह की दुआ माँगी। उसके बाद रूमियों की पराजय हुई और अरमानूस गिरफ़्तार हो गया। जब वह अल्प अर्सलान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उसके साथ बड़ा अच्छा सुलूक किया और इस शर्त पर उसे रिहा कर दिया कि वह भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर अपनी फ़ौज़ से अल्प अर्सलान की मदद किया करेगा और जितने मुसलमान उसकी क़ैद में हैं उन सबको रिहा कर देगा।
मलाज़गिर्द पूर्वी तुर्की में झील 'वान' के उत्तर में है। मलाज़गिर्द की जंग इतिहास की निर्णायक जंगों में गिनी जाती है। इसके नतीजे में पूरा एशिया-ए-कोचक मुसलमानों के क़बज़े में आ गया और यह भूभाग क्रमश: तुर्कों का देश बन गया।
अल्प अर्सलान ने दस साल हुकूमत की। वह बड़ा दानशील, नेक एवं न्यायप्रिय बादशाह था। उसके काल में सम्पूर्ण देश के फ़क़ीरों और ज़रूरतमंदों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे और हुकूमत की ओर से उनकी मदद की जाती थी।
एक बार अल्प अर्सलान को सूचना मिली कि उसके एक ग़ुलाम ने एक देहाती का तहबंद छीन लिया है तो अल्प अर्सलान ने इस अपराध में ग़ुलाम को सूली पर चढ़ा दिया। उसकी इस कठोरता का परिणाम यह था कि सम्पूर्ण देश में शान्ति एवं सुरक्षा क़ायम हो गई थी और अपराध समाप्त हो गए थे।
मलिक शाह (465 हि०/1072 ई० से 485 हि०/1092 ई०)
अल्प अर्सलान के बाद उसका लड़का मलिक शाह अठारह वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसके काल में सलजूक़ी सल्तनत अपने उत्थान पर पहुँच गई। पश्चिम में शाम (सीरिया) फ़तह हुआ और दक्षिण में यमन और अम्मान सलजूक़ी सल्तनत के अधीन आ गए और पूर्व में चीन तक सल्तनत की सीमा फैल गई। मलिक शाह ने बीस साल तक हुकूमत की। मलिक शाह सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सलजूक़ी हुक्मरान था। उसने प्रजा की सुविधा के लिए जनकल्याण के बहुत-से काम किए। बहुत-से टैक्स समाप्त कर दिए। जगह-जगह सड़कें बनवाईं, सराय और पुल का निर्माण करवाया।
उसे न्याय का बड़ा ख़याल था। उसके ज़माने में किसी पर ज़ुल्म नहीं हो सकता था, और यदि किसी पर ज़ुल्म हो जाता तो मज़लूम ख़ुद आकर मलिक शाह से फ़रियाद कर सकता था।
एक बार उसके फ़ौजियों ने एक विधवा की गाय पकड़कर ज़ब्ह कर दी। बुढ़िया को जब इसका पता चला तो वह शहर असफ़हान के उस पुल पर आकर खड़ी हो गई जहाँ से मलिक शाह गुज़रता था। जब बादशाह उस पुल पर से गुज़रा तो बुढ़िया ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, "बताओ तुम मेरा इनसाफ़ इस पुल पर करोगे या पुलसिरात पर?"
मलिक शाह घोड़े से उतर पड़ा और कहा, “पुलसिरात की मुझमें ताक़त नहीं, इसी पुल पर फ़ैसला करूँगा।"
अब बुढ़िया ने अपना क़िस्सा सुनाया। मलिक शाह ने बुढ़िया की फ़रियाद सुनकर अपराधी फ़ौजियों को कठोर दण्ड दिया और बुढ़िया को इनाम देकर मालामाल कर दिया।
मलिक शाह के न्याय एवं इनसाफ़ की ऐसी कई घटनाएँ इतिहास में मौजूद हैं।
निज़ामुल मुल्क तूसी
(408 हि०/1018 ई० से 485 हि०/1092 ई०)
मलिक शाह ने अपनी सल्तनत की सारी व्यवस्था अपने वज़ीर (मंत्री) निज़ामुल मुल्क को सौंप रखी थी। यह वज़ीर अपने गुणों के कारण बरामिका से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। सुल्तान अल्प अर्सलान के काल में भी वही वज़ीर था। उसकी बुज़ुर्गी के कारण मलिक शाह उसे 'बाबा' कहा करता था। निज़ामुल मुल्क का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उसने सल्तनत के प्रत्येक भाग में बड़े-बड़े मदरसे क़ायम किए जो उसके नाम पर 'निज़ामिया' कहलाते थे। उन मदरसों में सबसे बड़ा बग़दाद का मदरसा निज़ामिया था। उस मदरसे के ख़र्च के लिए बहुत बड़ी जायदाद वक़्फ़ (समर्पित) थी। मदरसे के निर्माण पर दो लाख दीनार ख़र्च हुए थे और तमाम विद्यार्थियों को वज़ीफ़ा (छात्रवृति) दिया जाता था।
मलिक शाह ने जब देखा कि निज़ामुल मुल्क मदरसों पर बेशुमार दौलत ख़र्च कर रहा है तो एक दिन उसने कहा, "बाबा! आप मदरसों पर जो रुपया ख़र्च कर रहे हैं यदि वह फ़ौज पर ख़र्च किया जाए तो दुनिया फ़तह की जा सकती है।"
निज़ामुल मुल्क ने जवाब दिया, “बेटा! तुम जो फ़ौज भर्ती करोगे उसके तीर चन्द गज़ से ज़्यादा दूर न जा सकेंगे, लेकिन मैं जो इल्मवालों (विद्वानों) की फ़ौज तैयार कर रहा हूँ उनकी दुआओं के तीर आसमान के भी पार चले जाएँगे।"
आलिमों और साहित्यकारों की क़द्रदानी के अलावा निज़ामुल मुल्क ग़रीबों एवं ज़रूरतमंदों की भी मदद करता था। वह दान भी बहुत करता था और अज़ान की आवाज़ सुनते ही सारा काम बंद कर देता और नमाज़ के लिए उठ जाता था।
निज़ामुल मुल्क की आदत थी कि जब वह घर से निकलता तो रुपयों की थैलियाँ ग़ुलामों के साथ होती थीं और रास्ते में जिस ज़रूरतमंद पर नज़र पड़ती, उसकी रुपयों से मदद करता था।
एक दिन उसकी सवारी किसी सब्ज़ी बेचनेवाले की दुकान की तरफ़ से निकली। वह सम्मान में उठ खड़ा हुआ और कहा कि मैं मुहताज हूँ। वर्तमान आमदनी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। निज़ामुल मुल्क ने ग़ुलाम की ओर इशारा किया। उसने एक थैली दे दी। सब्ज़ी बेचनेवाले ने उसपर दुआ दी और दुकान से उठकर दूसरे रास्ते पर जा बैठा और एक कपड़े से पाँव छुपाकर लंगड़ा बन गया, और निज़ामुल मुल्क से कहा कि मैं अपंग हूँ, लड़के-बच्चे अधिक हैं, रोटियों से मुहताज हूँ। वज़ीर ने ग़ुलाम की ओर इशारा किया। उसने फिर एक थैली दे दी। इस प्रकार सब्ज़ी बेचनेवाला नक़द रक़म लेकर यहाँ से भी उठा और आगे बढ़कर नए रूप में निज़ामुल मुल्क को सलाम करके कहने लगा कि मुझपर दुनिया तंग हो रही है (यानी मैं बहुत मुसीबत में हूँ)। छोटी-छोटी लड़कियों का बोझ सिर पर है। निज़ामुल मुल्क ने इस बार भी कुछ दे दिया। इसके बाद आवाज़ बदलकर चौथी बार सामने आया और कहने लगा कि मैं स्पीजाब का रहनेवाला हूँ और एक धर्म योद्धा (ग़ाज़ी) हूँ। अफ़सोस कि मेरी फ़ौज को पराजय हुई और बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ तक आया हूँ। इस बार भी निज़ामुल मुल्क ने इनाम का आदेश दिया, परन्तु यह कहते हुए कि ऐ सब्ज़ी फ़रोश, अपंग, लड़कियोंवाले और स्पीजाबी धर्म योद्धा (ग़ाज़ी) अपना इनाम ले।
निज़ामुल मुल्क के पास प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय आसानी से पहुँच सकता था। एक बार एक औरत शिकायत लेकर आई। निज़ामुल मुल्क उस समय दस्तरख़्वान पर था। संतरियों ने रोक दिया। निज़ामुल मुल्क को सूचना मिल गई। उसने संतरियों को चेतावनी दी और कहा “मैंने तुम्हें ग़रीबों और फ़रियादियों की सेवा के लिए रखा है। प्रतिष्ठित एवं गणमान्य लोग तो ख़ुद पहुँच जाते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति अनुमान कर सकता है कि जिस काल में बादशाह और वज़ीर ऐसे हों, जो ग़रीब से ग़रीब आदमी की शिकायत सुनने को तैयार रहते हों, तो उस काल में लोग कितनी शान्ति से रहते होंगे।
इस अच्छे वज़ीर को मलिक शाह के इंतिक़ाल के कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने जो बातिनी फ़िरक़ा ['बातिनी' एक इसमाईली फ़िरक़ा है। उन लोगों की आस्था है कि शरीअ़त में हर प्रत्यक्ष अर्थ का एक परोक्ष (बातिनी) अर्थ भी होता है। इसी कारण इस फ़िरक़ा को बातिनी कहा जाता है। सलजूक़ी काल में इस फ़िरक़ा का सबसे बड़ा रहनुमा हसन बिन सबाह (मृ० 1124 ई०) था। उसने मलिक शाह के अन्तिम काल में मीलान के पहाड़ों में एक स्थान पर जो 'अलमौत' कहलाता था, अपना एक गुप्त केन्द्र स्थापित कर रखा था। यहाँ उसने एक नक़ली जन्नत बनाई थी और क़ातिलों का एक गिरोह तैयार किया था जिनको 'फ़िदाई' कहा जाता था। हसन बिन सबाह जिन लोगों को अपने मज़हब के लिए ख़तरनाक समझता था उन्हें इन फ़िदाइयों के द्वारा क़त्ल करवा देता था। वह इन फ़िदाइयों को यह लालच देता था कि यदि तुम अपने मक़सद में कामयाब हो गए तो तुम्हें जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा और यह जन्नत वही होती थी जो उसने अलमौत में बनाई थी।
बातिनियों ने इस तरीक़े से बड़े-बड़े अग्रणी मुसलमानों को क़त्ल कर दिया। उनका सबसे बड़ा निशाना निज़ामुल मुल्क तूसी बना। प्रसिद्ध मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्द्दीन अय्यूबी पर भी उन्होंने हमला किया लेकिन वह बच गए। मलिक शाह के बाद सलजूक़ी सुल्तान संजर को भी उन्होंने क़त्ल की धमकी दी और प्रसिद्ध आलिम और क़ुरआन के मुफ़स्सिर इमाम राज़ी को भी क़त्ल करने की धमकी दी। मलिक शाह के बाद सलजूक़ियों का पतन प्रारंभ हुआ तो इन बातिनियों ने ईरान के बहुत-से पहाड़ी इलाक़ों में अपनी बाक़ायदा हुकूमत क़ायम कर ली। इस हुकूमत को 1256 ई० में मंगोल हुक्मरान हलाकू ख़ान ने ख़त्म किया और क़िला अलमौत को ढा दिया।] से सम्बन्ध रखता था, क़त्ल कर दिया। निज़ामुल मुल्क ने 'सियासत नामा' और 'दस्तूरुल वुज़रा' के नाम से दो किताबें लिखी थीं। ये किताबें जो फ़ारसी में हैं निज़ामुल मुल्क के राजनीतिक चिन्तन की श्रेष्ठ किताबें हैं और मुसलमानों के राजनीतिक दृष्टिकोण का उत्तम नमूना हैं।
अल्प अर्सलान और मलिक शाह के शासन काल पर, जबकि उनका प्रधानमंत्री निज़ामुल मुल्क तूसी था, एक अंग्रेज़ इतिहासकार सर पर्सी साइक्स ने इस प्रकार टिप्पणी की है :-
“ऐतिहासिक काल में एक विशाल एवं विस्तृत सल्तनत पर कभी इससे अच्छी हुकूमत नहीं की गई जैसी कि अल्प अर्सलान और मलिक शाह के तीस वर्षीय शासन काल में हुई।"
मलिक शाह के बाद उसके लड़कों महमूद और बरक्यारूक़ में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस आपस की लड़ाई में सल्तनत कमज़ोर हो गई और शाम, हिजाज़ और एशिया-ए-कोचक या तो सलजूक़ियों के क़बज़े से पूर्णतः निकल गए या केन्द्रीय हुकूमत की अधीनता से आज़ाद हो गए। सलजूक़ियों का ये गृह युद्ध इस्लामी दुनिया के लिए बड़ा हानिकारक साबित हुआ। इसके कारण एक ओर तुर्किस्तान और ख़ुरासान का इलाक़ा ग़ुज़ तुर्की ने तबाह व बरबाद कर दिया, दूसरी ओर फ़लस्तीन पर यूरोप की मसीही (ईसाई) क़ौमें क़ाबिज़ हो गईं और तीसरी ओर ख़ुद सलजूक़ी सल्तनत के भीतर बातिनियों की शक्ति बढ़ गई। अन्ततः तेरह साल के गृह-युद्ध के बाद मलिक शाह के एक लड़के मुहम्मद (498 हि०/1104 ई० से 511 हि०/1117 ई०) ने सलजूक़ी सल्तनत के बड़े हिस्से में पुनः एक ठोस हुकूमत क़ायम कर दी। अब सलजूक़ी सल्तनत इतनी विस्तृत तो नहीं थी जितनी मलिक शाह की थी, लेकिन फिर भी अपने काल की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इराक़, आरमीनिया, ईरान, तुर्किस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र अब भी इस सल्तनत में शामिल था।
सलजूक़ियों का अन्तिम शक्तिशाली हुक्मरान मुहम्मद का भाई संजर (511 हि०/1117 ई० से 552 हि०/1157 ई०) था। उसने चालीस साल से ज़्यादा हुकूमत की। तुर्किस्तान और ख़ुरासान का क्षेत्र उसकी हुकूमत में था और अन्य क्षेत्र यानी ईरान और इराक़ में उसके भाई और उनकी औलाद संजर की ओर से हुकूमत करते थे।
संजर एक न्याय प्रिय और नेक हुक्मरान था। वह ज्ञान एवं साहित्य को बहुत प्रोत्साहन देता था। उसके दरबार में साहित्य एवं शायरी की चर्चा वैसी ही रहती थी जैसी हारून रशीद, मामून रशीद और महमूद ग़ज़नवी के दरबारों में रहती थी। एक तत्कालीन इतिहासकार ने लिखा है—
"संजर आलिमों का सम्मान करता था, औलियाउल्लाह से श्रद्धा रखता था। उसके काल में ख़ुरासान दारुल-इल्म (ज्ञान का केन्द्र) बन गया और वहाँ के बड़े-बड़े शहर मदरसों, पुस्तकालयों, विद्वानों और विशेषज्ञों से भर गए।"
अमीर मुअज़ी (440 हि०/1048 ई० से 542 हि०/1147 ई०) और फ़ारसी का सबसे बड़ा क़सीदा कहनेवाला शायर अनवरी (मृत्यु -547 हि०/1152 ई०) उसके दरबारी शायर थे।
संजर अपनी विशाल सल्तनत पर आराम से हुकूमत कर रहा था कि 536 हि०/1140 ई० में उत्तर-पूर्व की ओर से एक ग़ैर मुस्लिम तुर्क क़ौम ने जो क़रा ख़िताई कहलाती थी, हमला कर दिया। संजर ने समरक़ंद के क़रीब मुक़ाबला किया, लेकिन पराजित हो गया और मावराउन-नहर का सारा इलाक़ा संजर के क़बज़े से निकल गया। संजर अब भी बाक़ी सल्तनत को सँभाले रहा, लेकिन बारह साल बाद एक नव मुस्लिम तुर्क क़बीला जो 'ग़ुज़' कहलाता था और बल्ख़ के निकट आबाद था, बाग़ी हो गया। संजर ने 548 हि०/1153 ई० में उनके मुक़ाबले में भी शिकस्त खाई और ग़ुज़ों के हाथों क़ैद हो गया।
ग़ुज़ों ने अपनी इस कामयाबी के बाद पूरे ख़ुरासान में तबाही मचा दी। लोगों का क़त्ले आम किया, मसजिदें और मदरसे ढा दिए और शहर एवं बस्तियाँ उजाड़ दीं। मंगोलों के आक्रमण से पूर्व इस्लामी काल में ख़ुरासान पर ऐसी तबाही कभी नहीं आई थी। ख़ुरासान की इस तबाही का शायर अनवरी ने एक कविता में, जो फ़ारसी भाषा की श्रेष्ठ कविताओं में गिनी गई है, बड़ा दर्दनाक चित्रण किया है। चार साल के बाद संजर ग़ुज़ों की क़ैद से रिहा हुआ। परन्तु इस रिहाई के तुरन्त बाद उसकी मृत्यु हो गई।
संजर के बाद सलजूक़ियों का पतन प्रारंभ हो गया था। अब ख़ुरासान और इराक़ भी उनके हाथ से निकल गए थे। हाँ उनका एक ख़ानदान किरमान में 583 हि०/1187 ई० तक, दूसरा ख़ानदान कुर्दिस्तान में 590 हि०/1194 ई० तक और तीसरा ख़ानदान एशिया-ए-कोचक में 700 हि०/1300 ई० तक हुकूमत करता रहा।
रूमी सलजूक़ी
इन छोटी-छोटी सलजूक़ी हुकूमतों में एशिया-ए-कोचक की हुकूमत जो रूमी सलजूक़ी के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी और बलवान थी।
इस हुकूमत का संस्थापक एक सलजूक़ी सरदार सुलैमान था जिसने 470 हि०/1077 ई० में तुर्की के उत्तर-पूर्वी भाग में नाईसिया के शहर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बना ली थी। प्रारंभ में यह हुकूमत मलिक शाह की केन्द्रीय हुकूमत के अधीन थी, लेकिन मलिक शाह की मृत्यु के बाद जो गृहयुद्ध हुए, उसमें आज़ाद हो गई।
रूमी सलजूक़ी का महत्त्व इस कारण है कि इस काल में यूरोप की क़ौमों ने मिलकर बैतुल मक़दिस पर क़बज़ा करने के लिए जो सलीबी जंगें शुरू कीं उनका पहला निशाना रूम के यही सलजूक़ी तुर्क बने। ये सलीबी लश्कर आम तौर पर एशिया-ए-कोचक के रास्ते शाम और फ़लस्तीन की तरफ़ जाते थे। सलजूक़ियों ने यूरोप की संगठित फ़ौजों के इन आक्रमणों का पूरी शक्ति से मुक़ाबला किया और इस प्रकार उन्होंने इस्लामी दुनिया की प्रतिरक्षा और विशेषकर बैतुल मक़दिस की सुरक्षा में बहुत सहयोग किया। यूरोप के पहले सलीबी आक्रमण में सुल्तान क़लीज अर्सलान सलजूक़ी (485 हि०/1092 ई० से 500 हि०/1106 ई०) ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया और यद्यपि सलजूक़ियों को नाईसिया का शहर छोड़ना पड़ा, परन्तु क़लीज अर्सलान ने सलीबी फ़ौज की बैतुल मक़दिस की ओर चढ़ाई में अधिक से अधिक रुकावट डाली और उन्हें कई बार पराजित किया। उसके इन कारनामों के कारण तुर्क क़लीज अर्सलान को अपना बहुत बड़ा 'हीरो' समझते हैं।
नाईसिया के बाद सलजूक़ियों की राजधानी क़ौनिया हो गया जो अन्तिम समय तक उनका हेडक्वार्टर रहा। रूमी सलजूक़ियों में अज़ीज़ुद्दीन कैकाऊस (606 हि०/1209 ई० से 616 हि०/1219 ई०) और अलाउद्दीन कैक़बाद प्रथम (616 हि०/1219 ई० से 634 हि०/1236 ई०) का काल सबसे शानदार था। उस काल में रूम की सलजूक़ी सल्तनत चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई और ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कृति की भी काफ़ी तरक़्क़ी हुई। प्रसिद्ध शायर जलालुद्दीन रूमी, अलाउद्दीन कैक़बाद के काल ही में क़ौनिया आकर आबाद हुए थे।
कारनामे
सलजूक़ियों की तीन राजधानियाँ थीं। तुग़रल की राजधानी शहर 'रै' थी, अल्प अर्सलान और संजर की 'मरू' और मलिक शाह की राजधानी 'असफ़हान'। इन तीनों शहरों ने इस काल में बड़ी तरक़्क़ी की। यहाँ आलीशान इमारतें निर्मित हुईं। मदरसे, शिफ़ाख़ाने और मसजिदें बनाई गईं। विशेषकर मरू ने काफ़ी तरक़्क़ी की और ज्ञान एवं साहित्य का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया। यहाँ के पुस्तकालय दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे।
सलजूक़ियों के काल में तरक़्क़ी के बड़े-बड़े काम हुए। क़ुर्दिस्तान और किरमान के प्रान्तों को जो बहुत पिछड़े हुए थे, विशेषकर बहुत तरक़्क़ी दी गई। उस काल में सीहून नदी से फ़ूरात नदी तक के विस्तृत इलाक़े में जिसमें तुर्किस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और इराक़ के देश सम्मिलित हैं, सौ साल तक पूर्ण शान्ति व्यवस्था बनी रही। इतिहास में इस क्षेत्र को ऐसी शान्ति बहुत कम मिली। प्रधानमंत्री निज़ामुल मुल्क ने इस बात पर गर्व करते हुए अपनी किताब सियासत नामा में लिखा है :-
“यद्यपि कुछ ख़लीफ़ाओं की सल्तनत इससे (सलजूक़ी सल्तनत से) अधिक विस्तृत थी लेकिन उनका काल किसी समय भी बग़ावतों से ख़ाली नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस ज़माने में कोई नहीं है जो बग़ावत का विचार दिल में लाए और आज्ञापालन से इनकार कर सके।”
ईरानी सलजूक़ियों के सम्बन्ध में कहा करते थे कि जिन वहशी तुर्कों से हमें भय लगता था और जिनकी हुकूमत को हम एक आफ़त समझते थे, उनके आने से मलिक की क़िस्मत बदल गई।
सलजूक़ियों का एक बड़ा कारनामा मदरसे क़ायम करना है। पहले शिक्षा की व्यवस्था मसजिद के अन्दर होती थी, परन्तु सलजूक़ी काल में योग्य प्रधानमंत्री निज़ामुल मुल्क ने मदरसों के लिए बाक़ायदा इमारतें बनाना प्रारंभ किया। अतः कुछ ही सालों में सरकारी सहायता से सारी सल्तनत में मदरसों का जाल बिछा दिया गया। सलजूक़ियों से पहले दुनिया के किसी हिस्से में इतनी तादाद में मदरसे कभी स्थापित नहीं किए गए थे।
सलजूक़ी काल में ज्ञान एवं साहित्य का भी बहुत विकास हुआ और इस्लामी दुनिया ज्ञान की दृष्टि से इस काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई। फ़ारसी भाषा का बहुत विकास हुआ और अब फ़ारसी गद्य में भी किताबें लिखी जाने लगीं। फ़ारसी कविता की दृष्टि से यह सुनहरा दौर है। अमीर मुअज़्ज़ा, अनवरी, निज़ामी और ख़ाक़ानी जो फ़ारसी भाषा के उच्च कोटि के शायर हुए हैं, इसी काल में थे। इनमें निज़ामी (535 हि०/1141 ई० से 599 हि०/1202 ई०) और ख़ाक़ानी (500 हि०/1107 ई० से 582 हि०/1185 ई०) गंजह के रहनेवाले थे जो आजकल आज़रबाइजान में है। उनका सम्बन्ध आज़रबाइजान के सलजूक़ी दरबार से था।
इमाम ग़ज़ाली (450 हि० से 505 हि०)
सलजूक़ी काल में जो विद्वान हुए हैं उनमें इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) (450 हि०/1059 ई० से 505 हि०/1111 ई०) का स्थान बहुत ऊँचा है। वे इस्लाम धर्म के बहुत बड़े विद्वान, सूफ़ी और दार्शनिक थे। वे नेशापुर के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, परन्तु उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में ऐसी तीव्र बुद्धि का प्रमाण दिया कि अट्ठाईस साल की आयु में ही उनकी विद्वता की प्रसिद्धि दूर-दूर तक पहुँच गई और वे अभी चौंतीस साल के भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री निज़ामुल मुल्क ने उन्हें बग़दाद के मदरसा निज़ामिया का सदर मुदर्रिस (प्रिंसिपल) नियुक्त कर दिया। बग़दाद में इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) का बहुत सम्मान हुआ और बड़े-बड़े अमीर एवं रईस उनके श्रद्धालुओं में सम्मिलित हो गए। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनकी महानता के सामने अमीरों, वज़ीरों और ख़ुद दरबारे ख़िलाफ़त की शान व शौकत भी मांद पड़ गई। इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) को यद्यपि दुनियावी दृष्टि से बड़ी महानता प्राप्त हो गई थी, परन्तु उनका दिल संतुष्ट नहीं था। वह उस काल के आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज और विचारों से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि नैतिक एवं बौद्धिक दृष्टि से मुसलमानों की हालत ख़राब हो गई थी, और मुसलमानों का जीवन प्रारंभिक काल [वह दौर जब सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ताबिईन और तबा ताबिईन ज़िन्दा थे। यह ज़माना दूसरी सदी हिजरी के आख़िर में यानी हारून रशीद के ख़िलाफ़त के अन्तिम दौर में समाप्त हो जाता है।] के समान मिसाली नहीं रहा है। इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) की अमीर और ग़रीब दोनों से शिकायत थी। वे हक़ को तलाश करना चाहते थे। उनका यह असंतोष इतना बढ़ गया कि एक दिन सब कुछ छोड़कर बग़दाद से निकल खड़े हुए। उन्होंने ग्यारह साल तक शाम (सीरिया), फ़िलस्तीन और हिजाज़ के पवित्र स्थलों, मसजिदों और रेगिस्तानों में तन्हाई की ज़िन्दगी गुज़ारकर इबादत की और विचार-विमर्श में समय व्यतीत किया। अल्लाह ने उनकी यह मेहनत स्वीकार की और उनके दिल को संतुष्टि प्रदान कर दी। वे अन्ततः इस नतीजे पर पहुँचे कि दुनिया में नुबूवत के इल्म से बढ़कर कोई इल्म नहीं, जिससे रौशनी हासिल की जाए। अब उन्होंने परिश्रम और रेगिस्तानों में एकांतवास त्याग दिया और बग़दाद वापस आकर लोगों का सुधार और लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने श्रेष्ठ किताबें लिखकर उन गुमराहियों को दूर किया जिनमें बहुत-से मुसलमान विद्वान यूनानी दर्शन से प्रभावित थे। इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) ने दर्शनशास्त्र से लाभप्रद काम लिया और उससे इस्लामी आस्थाओं और दृष्टिकोणों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हुकूमत में, बादशाहों में, प्रशासनिक पदाधिकारियों में, व्यापारियों में, आलिमों (विद्वानों) और आम लोगों में कैसी-कैसी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं और ये सब लोग इस्लाम की सही शिक्षा से कितने दूर जा चुके हैं। इमाम ग़ज़ाली की किताबों ने एक क्रान्ति ला दी और उनसे लोगों को अपनी ज़िन्दगी सँवारने में बड़ी मदद मिली। उनके एक शार्गिद (शिष्य) इब्ने तूमर्त ने मराकश पहुँचकर उनकी विचारधारा के आधार पर एक हुकूमत की बुनियाद भी डाल दी जो 'ख़िलाफ़ते मुवह्हिदीन' कहलाती है। इसका उल्लेख आगे आएगा।
इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) कई सौ किताबों के रचयिता हैं। दुनिया के बहुत कम लेखकों ने इतनी अधिक तादाद में और इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब 'इह्याउल-उलूम' है। इस किताब का मुसलमानों के जीवन पर सदियों तक प्रभाव रहा। यूरोप के दार्शनिकों एवं विद्वानों के विचार भी इस किताब से प्रभावित हुए। मूल पुस्तक अरबी में है, परन्तु इसका उर्दू में अनुवाद हो चुका है। इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) ने ईरानियों के लिए, जिनकी ज़बान फ़ारसी थी, फ़ारसी में भी एक किताब लिखी। इस किताब का भी उर्दू में 'कीमया-ए-सआदत' के नाम से अनुवाद हो गया है। इस किताब में इह्याउल-उलूम के विचारों को संक्षप्ति और सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह)
(470 हि०/1077 ई० से 561 हि०/1166ई०)
सलजूक़ी काल की इल्मी दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती मशहूर वली अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) की है। उनके बचपन की एक घटना, कि उन्होंने अपनी माँ के आदेश पर किस प्रकार अमल किया और डाकुओं के सामने भी झूठ नहीं बोले, बहुत प्रसिद्ध है और इस्लामी दुनिया का बच्चा-बच्चा उससे परिचित है। अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) वली होने के अलावा एक बहुत बड़े सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों के माध्यम से लोगों का सुधार किया। कहा जाता है कि उनके हाथ पर पाँच हज़ार ईसाई और यहूदी इस्लाम लाए और एक लाख मुसलमानों ने उनके सामने बुरे काम न करने का वचन दिया।
वे बड़े बेबाक और साहसी थे। बड़े से बड़े आदमी को भी टोक देते थे। एक बार बग़दाद में ख़लीफ़ा ने एक अत्याचारी व्यक्ति को क़ाज़ी नियुक्त कर दिया। अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) को जब मालूम हुआ तो एक सार्वजनिक सभा में इसका विरोध किया और ख़लीफ़ा से कहा—
“तुमने एक अत्याचारी को क़ाज़ी नियुक्त कर दिया। जब तुमसे ख़ुदा पूछेगा तो क्या जवाब दोगे?"
ख़लीफ़ा को जब मालूम हुआ तो उसने क़ाज़ी को तुरन्त बरतरफ़ कर दिया।
अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) बादशाह नहीं थे, परन्तु उनकी दानशीलता बादशाहों से भी अधिक थी। उनके श्रद्धालु उन्हें जो कुछ देते थे वह सब भूखों और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च कर देते थे। वे कहा करते थे कि यदि सारी दुनिया की दौलत मेरे क़बज़े में हो तो सारी की सारी दौलत मैं भूखों और ग़रीबों पर ख़र्च कर दूँ।
उमर ख़य्याम (440 हि०/1048 ई० से 526 हि०/1132 ई०)
फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि उमर ख़य्याम जिनकी रुबाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, वे भी इसी सलज़ूक़ी काल में हुए। वे मलिक शाह और संजर के काल में थे। ख़य्याम एक कवि की हैसियत से प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने ज़माने के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने एक कैलेण्डर तैयार किया था जो 'तक़्वीम-जलाली' कहलाता था। यह कैलेण्डर अंग्रेज़ी के वर्तमान कैलेण्डर से भी अधिक शुद्ध था। इसके अलावा गणित की एक शाखा 'बीजगणित' में मुसलमानों की ओर से अन्तिम वृद्धि उमर ख़य्याम ने ही की।
सलजूक़ी काल के एक विशिष्ट व्यक्ति जलालुद्दीन रूमी (604 हि०/1207 ई० से 672 हि०/1273 ई०) हैं। उनका सम्बन्ध सलजूक़ियों के उस काल से है जब उनकी हुकूमत सिर्फ़ एशिया-ए-कोचक में रह गई थी। मौलाना रूमी पैदा तो बल्ख़ में हुए थे, परन्तु जब बाईस वर्ष की उम्र हुई तो अपने पिता के साथ एशिया-ए-कोचक के शहर क़ौनिया में जाकर बस गए थे। एशिया-ए-कोचक का इलाक़ा उस ज़माने में रूम के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए वे मौलाना रूम कहलाते हैं। क़ौनिया में उन्होंने एक किताब लिखी जो 'मसनवी' कहलाती है। यह किताब शायरी (पद्य) में है और शाहनामा की तरह आज तक शौक़ से पढ़ी जाती है। परन्तु 'मसनवी' में शाहनामा की तरह बेसिर-पैर की बातें नहीं हैं, बल्कि उसमें बुद्धिमानी एवं विवेक की बातें हैं।
इन व्यक्तित्वों के अलावा सलजूक़ी काल में और भी कई महान लेखक और रचनाकार हुए हैं जिन्होंने ज्ञान एवं कला के क्षेत्र में नई-नई दिशाओं की खोज की और जिनके नाम आज भी ज़िन्दा हैं। जारुल्लाह ज़मख़्शरी (मृत्यु - 538 हि०/1144 ई०) जो शब्दकोष और साहित्य के विशेषज्ञ थे, वे कश्शाफ़ के नाम से क़ुरआन की एक तफ़सीर के लेखक भी हैं, जो बौद्धिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट तफ़सीर समझी जाती है।
मुहम्मद बिन अब्दुल करीम शहरस्तानी (469 हि०/1076 ई० से 548 हि०/1153 ई०) अपने काल के तर्कशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी किताबों में सबसे प्रसिद्ध 'अलमिलल-वन-नहल' है जिसमें उन्होंने अपने ज़माने के तमाम मज़हबों और दार्शनिक मान्यताओं से बहस की है।
उस काल के विद्वानों में उमर ख़य्याम के बाद सबसे प्रमुख व्यक्तित्व 'ख़ाज़नी' की है और उनकी किताब 'मीज़ानुल हिक्मत' मध्य काल में जीव-विज्ञान पर लिखी गई किताबों में प्रथम श्रेणी की किताब समझी जाती है। ख़ाज़नी ने नक्षत्र अवलोकन भी किए और अपने अनुभवों को एक किताब में लिख दिया, जो 'ज़ीच संजरी' कहलाती है। ख़ाज़नी संजर के काल में थे।
साहित्यकारों में हरीरी (446 हि०/1054 ई० से 516 हि०/1122 ई०) का नाम बहुत प्रमुख है। उसकी किताब 'मक़ामात' अरबी लेखमाला का उत्कृष्ट नमूना है। ग़ज़नवी काल में हमदानी ने जो लेखशैली प्रारंभ की थी, हरीरी ने उसे विकसित किया। हरीरी इराक़ का वासी था।
उस काल के एक और महान व्यक्ति अब्दुल्लाह अनसारी (396 हि०/1006 ई० से 481 हि०/1088 ई०) हैं जो 'पीरे हरात' के नाम से प्रसिद्ध थे। वे आलिम, सूफ़ी और शायर थे। उनकी सूफ़ियाना शायरी ने बाद के उच्च स्तर के सूफ़ी शायरों, जैसे सनाई और रूमी, पर बहुत प्रभाव डाला। उनके 'रिसाला-मुनाजात' के बारे में एक अंग्रेज़ी आलोचक ने लिखा है कि यह किताब ज्ञान एवं विवेक और ईश-परायणता का ख़ज़ाना है।
समाज
सलजूक़ी काल के इन तमाम कारनामों के साथ एक दूसरा पहलू भी उल्लेखनीय है और वह यह कि सम्पूर्ण राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकासों के बावजूद इस काल में नैतिक रूप से मुसलमानों का पतन प्रारंभ हो गया था। पाँच सौ साल की लगातार तरक़्क़ी और धन-दौलत की बहुलता ने स्वार्थ भाव पैदा कर दिया और जब स्वार्थ-भाव पैदा हुआ तो लोग दूसरों का हक़ मारने लगे और इस प्रकार मुसलमानों में बेईमानी और दूसरी नैतिक बुराइयाँ पैदा हो गईं, जिनसे हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) डरते थे और जिसका इज़हार आपने उस वक़्त किया था जब मदाइन की फ़तह के बाद 'किसरा' का ख़ज़ाना मदीना पहुँचा था।
इसके अलावा ग़ैर इस्लामी दर्शन एवं धर्मों की किताबों के अरबी में अनुवाद हो जाने से मुसलमानों के अक़ीदे (आस्थाएँ) भी प्रभावित हुए और उनमें गुमराह करनेवाले विचार फैलने लगे। इस बात ने एक वर्ग में इस्लाम पर ईमान को कमज़ोर कर दिया और जब ईमान कमज़ोर हो गया तो अमल में भी फ़र्क़ पड़ा।
सलजूक़ी काल के लेखकों की रचनाओं से हमें इस नैतिक पतन का पता चलता है। अत: इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी प्रसिद्ध किताब इह्याउल-उलूम में लिखा है—
"प्रजा इस कारण बदहाल हो गई कि बादशाहों की हालत बिगड़ गई और बादशाहों की हालत इस कारण बिगड़ी कि आलिमों की हालत बिगड़ गई और आलिमों के अन्दर ख़राबी इस वजह से है कि पद एवं प्रतिष्ठा के प्रेम ने उनके दिलों पर परदा डाल दिया है।"
सलजूक़ी सल्तनत
उत्थान काल
(429 हि०/1037 ई० से 552 हि०/1157 ई०)
1. तुग़रिल - 429 हि०/1037 ई० से 455 हि०/1063 ई०
2. अल्प अर्सलान - 455 हि०/1063 ई० से 465 हि०/1072 ई०
3. मलिक शाह - 465 हि०/1072 ई० से 485 हि०/1092 ई०
4. महमूद - 485 हि०/1092 ई० से 487 हि०/1094 ई०
5. बरक्यारूक़ - 487 हि०/1094 ई० से 498 हि०/1104 ई०
6. मुहम्मद - 498 हि०/1104 ई० से 511 हि०/1117 ई०
7. संजर - 511 हि०/1117 ई० से 552 हि०/1157 ई०
मलाज़गिर्द की जंग - 465 हि०/1072 ई०
अब्बासी ख़लीफ़ा
(जो बनी बुवैह और सलजूक़ी हुक्मरानों के अधीन थे)
1. मस्तकफ़ी बिल्लाह - 333 हि०/944 ई० से 334 हि०/945 ई०
2. मुतै'अ लिल्लाह - 334 हि०/945 ई० से 363 हि०/974 ई०
3. ताए लिल्लाह - 363 हि०/974 ई० से 381 हि०/991 ई०
4. क़ादिर बिल्लाह - 381 हि०/991 ई० से 422 हि०/1031 ई०
5. क़ायम-बअमरिल्लाह - 422 हि०/1031 ई० से 467 हि०/1074 ई०
(इस ख़लीफ़ा के काल में तुग़रल 447 हि०/1055 ई० में बग़दाद में दाख़िल हुआ और बनी बुवैह का आधिपत्य समाप्त हो गया।)
6. मुक़तदी बअमरिल्लाह - 467 हि०/1074 ई० से 487 हि०/1094 ई०
7. मुस्तहज़र बिल्लाह - 487 हि०/1094 ई० से 512 हि०/1118 ई०
8. मुस्तरशिद बिल्लाह - 512 हि०/1118 ई० से 529 हि०/1134 ई०
9. राशिद बिल्लाह - 529 हि०/1134 ई० से 530 हि०/1135 ई०
10. मुकतफ़ी बिल्लाह - 530 हि०/1135 ई० से 555 हि०/1160 ई०
(इसके काल में 547 हि०/1152 ई० में अब्बासी ख़लीफ़ा सलजूक़ी सत्ता की अधीनता से आज़ाद हो गए।)
अध्याय-16
पठान कर्मभूमि में
ग़ज़नी की सल्तनत के पतन के बाद ग़ौरी ख़ानदान की जो हुकूमत क़ायम हुई वह हालाँकि मात्र पचास साल चली, लेकिन इस्लामी इतिहास में उसे इस कारण महत्त्व प्राप्त है कि उसके ज़माने में उत्तर-पूर्व भारत में पहली बार इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पड़ी।
ग़ौरी ख़ानदान की हुकूमत को इतिहास में 'आले शंसब' की हुकूमत भी कहा जाता है। प्रारंभ में यह ख़ानदान ग़ज़नी की हुकूमत को टैक्स देता था और काबुल एवं हरात के मध्य ग़ौर के पहाड़ी इलाक़े पर इसकी हुकूमत थी। इस इलाक़े का केन्द्र 'फ़िरोज़ कोह' था। ग़ौर के निवासी नस्ल से पठान थे। अब तक इस्लामी इतिहास में जिन क़ौमों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे अरब, ईरानी, तुर्क और बर्बर थे। ग़ौरियों के शासनकाल में पठान पहली बार इस्लामी इतिहास में एक महान क़ौम की हैसियत से पहचाने गए।
सुल्तान इबराहीम ग़ज़नवी (451 हि०/1059 ई० से 492 हि०/1099 ई०) के बाद ग़ौर के हुक्मरान मलिक अज़ीज़ुद्दीन हुसैन ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली। उसके बाद उसका बेटा सैफ़ुद्दीन सूरी हुक्मरान हुआ। उसने बहराम शाह ग़ज़नवी (512 हि०/1118 ई० से 547 हि०/1152 ई०) के काल में ग़ज़नी पर आक्रमण किया और शहर पर क़बज़ा करके सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। लेकिन बहराम शाह ने जल्द ही ग़ज़नी को उससे छीन लिया और सैफ़ुद्दीन को क़त्ल करवा दिया। जब सैफ़ुद्दीन के भाई अलाउद्दीन हुसैन को, जिसे बाद में 'जहाँसोज़' के नाम से पुकारा गया, सूचना मिली तो उसने भाई का बदला लेने के लिए ग़ज़नी पर हमला कर दिया। शहर को आग लगा दी और सात दिन तक क़त्लेआम किया।
551 हि०/1156 ई० में अलाउद्दीन 'जहाँसोज़' की मृत्यु हो गई। ग़ौर के इलाक़े में अब तक करामता और इस्माइली सम्प्रदाय का बहुत प्रभाव था। अलाउद्दीन 'जहाँसोज़' भी इसी आस्था में विश्वास रखता था। लेकिन जब उसका लड़का सैफ़ुद्दीन द्वितीय, जो सच्चा मुसलमान था, गद्दी पर बैठा तो उसने ग़ौर के इलाक़े से करामता का प्रभाव समाप्त कर दिया।
ग़ौरी ख़ानदान ने वास्तविक प्रतिष्ठा दो भाइयों ग़यासुद्दीन और शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी के काल में प्राप्त की जो सैफ़ुद्दीन द्वितीय के चचाज़ाद भाई थे और सैफ़ुद्दीन की मृत्यु के बाद क्रमश: उत्तराधिकारी बने। ग़यासुद्दीन ग़ौरी ने (567 हि०/1171 ई०) में ग़ज़नी को स्थायी रूप से जीत लिया और शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी को सुल्तान माज़ुद्दीन की उपाधि देकर ग़ज़नी की गद्दी पर बैठा दिया। ग़यासुद्दीन ने इस दौरान हरात और बल्ख़ भी जीत लिए और हरात को अपनी राजधानी घोषित किया।
सुल्तान शहाबुद्दीन ग़ौरी हालाँकि अपने भाई का सहयोगी था, परन्तु उसने ग़ज़नी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और पाकिस्तान और उत्तरी भारत को फ़तह करके इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त किया। 598 हि०/1202 ई० में अपने भाई की मृत्यु के बाद वह सम्पूर्ण ग़ौरी सल्तनत का हुक्मरान बन गया।
ग़ज़नी का इलाक़ा पाकिस्तान की सरहद से मिला हुआ था। इसलिए शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी की फ़ौजी कार्रवाइयाँ इस क्षेत्र से प्रारंभ हुईं और वह जगप्रसिद्ध दर्रा ख़ैबर से ज़्यादा दर्रा गोमल के रास्ते पाकिस्तान में दाख़िल हुआ। उसने सबसे पहले मुल्तान और ओछ पर हमले किए जो ग़ज़नवियों के पतन के बाद एक बार फिर इसमाईली सम्प्रदाय के गढ़ बन गए थे। ये इसमाईली एक ओर मिस्र के फ़ातिमी ख़लीफ़ाओं के साथ और दूसरी ओर भारत के हिन्दुओं से निकट सम्बन्ध बनाए हुए थे। ग़ौर के हुक्मरान आम मुसलमानों की तरह अब्बासी ख़िलाफ़त को स्वीकार करते थे और वे इसमाईलियों की सरगर्मियों को मुसलमानों के हित के ख़िलाफ़ समझते थे। मुहम्मद ग़ौरी ने 571 हि०/1175 ई० में मुल्तान और ओछ दोनों शहर फ़तह कर लिए, उसके बाद 575 हि०/1179 ई० में मुहम्मद ग़ौरी ने पेशावर और 576 हि०/1180 ई० में दैवल को फ़तह करके ग़ौरी सल्तनत की सीमाएँ अरब सागर तक बढ़ा दीं। लाहौर और उससे लगे हुए इलाक़े अभी तक ग़ज़नवी ख़ानदान के अधीन थे, जिनकी हुकूमत ग़ज़नी पर 'जहाँसोज़' के हमले के बाद लाहौर आ गई थी। शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी ने 582 हि०/1186 ई० में लाहौर पर क़बज़ा करके ग़ज़नवी ख़ानदान की हुकूमत को पूर्णत: समाप्त कर दिया।
लाहौर और पश्चिमी पाकिस्तान को जीतने के बाद शहाबुद्दीन ने भटिंडा को फ़तह किया जो पहले ग़ज़नवी सल्तनत में सम्मिलित था, परन्तु उस समय दिल्ली और अजमेर हिन्दू राजा पृथ्वीराज के क़बज़े में था। पृथ्वीराज ने जब यह सुना कि शहाबुद्दीन ग़ौरी ने भटिंडा फ़तह कर लिया, तो वह एक ज़बर्दस्त फ़ौज लेकर, जिसकी तादाद दो लाख थी, मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में करनाल के निकट तलावड़ी के मैदान में दोनों फ़ौजों में लड़ाई हुई, परन्तु शहाबुद्दीन की फ़ौज थोड़ी थी, पराजित हुई और शहाबुद्दीन बुरी तरह घायल हो गया। इसी हालत में एक सिपाही उसे बचाकर ले गया। शहाबुद्दीन को इस पराजय का इतना दुख हुआ कि एक वर्ष तक उसने ऐशो आराम की ज़िन्दगी नहीं गुज़ारी। उसके बाद एक बड़ी फ़ौज लेकर विगत पराजय का बदला लेने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इधर से पृथ्वीराज भी भारत के दो ढाई सौ राजाओं की मदद से एक बड़ी फ़ौज लेकर रवाना हुआ। इस बार भी मुक़ाबला तलावड़ी के मैदान में हुआ परन्तु शहाबुद्दीन ग़ौरी को फ़तह हुई। पृथ्वीराज लड़ाई में मारा गया।
पृथ्वीराज को पराजित कर शहाबुद्दीन ने दिल्ली और अजमेर भी जीत लिया और उसके सिपहसालार बख़तियार ख़िलजी ने आगे बढ़कर बिहार और बंगाल भी जीत लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत और पाकिस्तान मुसलमानों के क़बज़े में आ गया।
हिन्दुस्तान और बंगाल में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक और एक होशमंद हुक्मरान की हैसियत से शहाबुद्दीन को उच्च स्थान प्राप्त है। उसकी युद्ध सफलता महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों के मुक़ाबले में ज़्यादा लाभदायक साबित हुई। वह महमूद की तरह किसी इलाक़े को जीतकर वापिस नहीं जाता था, बल्कि उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था। उसने बर कोचक, पाकिस्तान एवं भारत में मुसलमानों की स्थायी हुकूमत स्थापित कर दी और इस प्रकार वह काम पूरा कर दिया जो पाँच सौ साल पहले मुहम्मद बिन क़ासिम ने शुरू किया था।
शहाबुद्दीन के काल में ग़ैर मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में इस्लाम क़बूल किया। झेलम नदी और सिंध के बीच 'खोखर' नामक एक क़ौम आबाद थी। उनके यहाँ एक मुसलमान क़ैद था। यह मुसलमान उन लोगों को इस्लाम की ख़ूबियाँ बताता रहता था जिसे वे लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। एक दिन उनके सरदार ने कहा—
“यदि मैं मुसलमान हो जाऊँ तो तुम्हारा बादशाह मेरे साथ क्या सुलूक करेगा?"
मुसलमान क़ैदी ने जवाब दिया, “यदि तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बादशाह तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेगा।"
खोखर के सरदार ने जब यह बात सुनी तो इस्लाम ले आया। मुसलमान ने एक ख़त के द्वारा अपनी बातचीत की सूचना सुल्तान शहाबुद्दीन को दे दी। शहाबुद्दीन ने उसके जवाब में सरदार को इनाम एवं भेंट दिया और उस इलाक़े की जागीर भी उसे दे दी।
इसके बाद उसकी क़ौम ने भी इस्लाम क़बूल कर लिया। इस्लाम क़बूल करने से पहले खोखर बहुत-सी बुराइयों में लिप्त थे। उनमें एक बुराई थी कि वे जाहिलियत काल के अरबों की तरह लड़कियों को क़त्ल कर दिया करते थे। इस्लाम लाने के बाद यह बुरी रस्म भी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाक़ों के पठान भी उसी काल में इस्लाम लाए।
इस पूरी अवधि में शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी का भाई ग़यासुद्दीन हरात पर हुकूमत करता रहा। उसने हरात के शहर को बहुत विकसित किया और वहाँ एक शानदार जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जो आज भी मौजूद है और शहर हरात की सबसे प्रमुख और बड़ी इमारत है। ग़यासुद्दीन ने 46 साल हुकूमत की और 598 हि०/1202 ई० में उसकी मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी हरात में भाई के स्थान पर सम्पूर्ण ग़ौरी सल्तनत का बादशाह हो गया।
यह वह काल है जब सलजूक़ियों के बाद ख़ुरासान और तुर्किस्तान पर ख़्वारिज़्म शाही ख़ानदान की हुकूमत क़ायम हो गई थी। ग़ौरियों की इस ख़ानदान से लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थीं। ग़यासुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन के काल में भी ये लड़ाइयाँ जारी रहीं। इन लड़ाइयों के सिलसिले में शहाबुद्दीन 601 हि०/1204 ई० में ख़्वारिज़्म तक पहुँच गया, परन्तु वहाँ उसे पराजय हुई और यह अफ़वाह फैल गई कि मुहम्मद ग़ौरी जंग में काम आ गया। इस ख़बर के फैलते ही पंजाब के खोखरों ने बग़ावत कर दी। मुहम्मद ग़ौरी तुरन्त पंजाब आया और बग़ावत को दबा दिया परन्तु बग़ावत को समाप्त करने के बाद जब वह वापस जा रहा था तो झेलम नदी के किनारे एक इसमाईली फ़िदाई ने हमला करके उसे शहीद कर दिया। शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी की मौत के साथ ही ग़ौरी ख़ानदान की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। हरात और ग़ज़नी के इलाक़ों पर ख़्वारिज़्म शाह की हुकूमत क़ायम हो गई और पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान में मुहम्मद ग़ौरी के वफ़ादार ग़ुलाम क़ुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली में सुल्तान का सहयोगी था, एक स्थायी इस्लामी हुकूमत क़ायम कर ली।
ग़ौरियों के काल के आलिमों में इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी (543 हि०/1149 ई० से 606 हि०/1209 ई०) का नाम प्रमुख है। वह पैदा तो शहर रै में हुए थे, लेकिन ज़िन्दगी के आख़िरी 24 साल ग़ज़नी और हरात में गुज़ारे। हरात में उनके लिए एक मदरसा क़ायम कर दिया गया था, जहाँ वह दर्स देते थे। इमाम राज़ी ने तर्कशास्त्र और फ़िक़्ह में कई अहम किताबें लिखीं, परन्तु उनकी प्रसिद्धि 'तफ़सीरे कबीर' के कारण है जो क़ुरआन की उच्चकोटि की तफ़सीरों में गिनी जाती है। सुल्तान ग़यासुद्दीन ग़ौरी के धार्मिक विश्वासों के सुधार में इमाम राज़ी का बड़ा हाथ है। उनके सुधार-कार्य के कारण 'बातिनी' उनके दुश्मन हो गए। ग़ौरी-काल के दूसरे प्रमुख व्यक्ति ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती (रहमतुल्लाह अलैह) (मृत्यु 633 हि०/1235 ई०) हैं। वे शहाबुद्दीन ग़ौरी के साथ हिन्दुस्तान आए और अजमेर में निवास किया और वहाँ के ग़ैर मुस्लिमों में इस्लाम फैलाया।
ग़ौरी सल्तनत
(552 हि०/1157 ई० से 602 हि०/1206 ई०)
ग़यासुद्दीन ग़ौरी - 552 हि०/1157 ई० से 598 हि०/1202 ई०
शहाबुद्दीन ग़ौरी - 598हि०/1202 ई० से 602 हि०/1206 ई०
तलावड़ी की पहली जंग - 587 हि०/1191 ई०
तलावड़ी की दूसरी जंग - 588 हि०/1192 ई०
दिल्ली पर विजय - 588 हि०/1192 ई०
बंगाल (बंगला देश) पर विजय - 595 हि०/1198 ई०
मालवा पर विजय - 596 हि०/1199 ई०
ग्वालियर पर विजय - 597 हि०/1200 ई०
काल्पी और कालिंजर पर विजय - 598 हि०/1202 ई०
अध्याय-17
हिलाल और सलीब की कशमकश
जिस प्रकार हम अरब को एक पवित्र मुल्क समझते हैं क्योंकि यहाँ इस्लाम का प्रारंभ हुआ और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ज़िंदगी गुज़ारी, उसी प्रकार ईसाई फ़िलस्तीन के शहर बैतुल मक़दिस को पवित्र शहर समझते हैं, क्योंकि वहाँ से ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ और वहीं हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ने ज़िंदगी गुज़ारी। बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों ने हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के काल में बिना किसी लड़ाई के समझौते के द्वारा क़बज़ा किया था, जिसकी चर्चा हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के हालात में की जा चुकी है। यह क़बज़ा सलजूक़ियों के समय तक क़ायम रहा, परन्तु मलिक शाह की मृत्यु के बाद जब सलजूक़ियों का पतन हुआ तो शाम (सीरिया) और एशिया-ए-कोचक एक बार फिर छोटी-छोटी हुकूमतों में बँट गए। ये हुकूमतें आपस में लड़ा करती थीं। उसी ज़माने में बैतुल मक़दिस पर फ़ातिमी हुकूमत का पुनः क़बज़ा हो गया। जब ईसाइयों ने मुसलमानों की यह कमज़ोरी देखी तो उन्होंने फ़िलस्तीन को मुलमानों के क़बज़े से वापस लेने की कोशिश शुरू कर दी। फ़िलस्तीन और विशेषकर बैतुल मक़दिस पर क़बज़ा करने के लिए ईसायसों ने जो लड़ाइयाँ लड़ीं वह 'सलीबी जंगें' कहलाती हैं। [इन सलीबी जंगों की तादाद जो बैतुल मक़दिस हासिल करने के लिए यूरोपवालों ने लड़ीं कुल आठ हैं :-
(i) पहली जंग (1096 से 1099 ई०) - यूरोप की संयुक्त फ़ौजों ने बैतुल मक़दिस, फ़िलस्तीन और शाम (सीरिया) के समुद्री तट के इलाक़े फ़तह कर लिए।
(ii) दूसरी जंग (1147 ई०- 1149 ई०) - अमादुद्दीन ज़ंगी की कामयाबियों को रोकने के लिए लड़ी गई। इस जंग का नेतृत्व जर्मनी के शहंशाह कोनराड तृतीय और फ़्रांस के बादशाह लुई तृतीय ने किया। अमादुद्दीन की मृत्यु हो गई थी इसलिए उसके लड़के नूरुद्दीन ज़ंगी को इस संयुक्त फ़ौज का मुक़ाबला करना पड़ा, परन्तु सलीबियों को सफलता नहीं मिली।
(iii) तीसरी जंग (1189 से 1192 ई०) - यह सबसे बड़ी और मशहूर जंग है। यह उस वक़्त शुरू की गई जब सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दिस फ़तह कर लिया। इसका नेतृत्व ब्रिटेन के रिचर्ड शेरवील, फ़्रांस के बादशाह फ़िलिप और जर्मनी के शहंशाह फ़्रेडरिक बारब्रोसा ने किया। फ़्रेडरिक एशिया-ए-कोचक में एक नदी में डूब गया। रिचर्ड और फ़िलिप भी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सके।
(iv) चौथी जंग (1201 ई०-1204 ई०) - इस जंग में यूरोप की सलीबी फ़ौज आपस में लड़ पड़ी। यूरोप के शहरों में ख़ून-ख़राबा किया और बैतुल मक़दिस की बजाए यूरोप के मसीही शहर क़ुस्तनतीनिया को फ़तह किया।
(v) पाँचवी जंग (1218 ई० 1221ई०) - इस जंग के दौरान यूरोप की सलीबी फ़ौजों ने मिस्र पर हमला किया। मलिक कामिल अय्यूबी ने उन्हें पराजित किया।
(vi) छठी जंग (1228 ई०-1229 ई०) - जर्मनी का शहंशाह फ़्रेडरिक द्वितीय इस अभियान का नेता था। जंग नहीं हुई और मलिक कामिल ने आपसी समझौते से बैतुल मक़दिस ईसाइयों को सौंप दिया, परन्तु मलिक कामिल के बाद मुसलमानों ने शहर वापस ले लिया।
(vii) सातवीं जंग (1248 ई०-1249 ई०) - इसका नेतृत्व फ़्रांस के लुई नवम् ने किया। मिस्र पर हमला किया गया। मलिक अस-सालेह अय्यूबी ने मुक़ाबला किया। लुई गिरफ़्तार हो गया और बाद में फ़िदया देकर रिहा हुआ।
(viii) आठवीं जंग (1270 ई० 1271 ई०) - लुई नवम् ने रिहाई के बाद फिर एक कोशिश की। इस बार इंग्लैण्ड का शाह एडवर्ड भी सम्मिलित था, परन्तु रुख़ तूनिस (Tunish) का किया और वहीं लुई की मृत्यु हुई। इस प्रकार आख़िरी सलीबी जंग भी असफल रही।
इन लड़ाइयों के अतिरिक्त एक और जंग उल्लेखनीय है जो 'बच्चों की सलीबी जंग' कहलाती है। यूरोपवालों का विचार था कि बड़े लोग चूँकि गुनाहों के काम करते हैं इसलिए ख़ुदा उन्हें मुसलमानों के मुक़ाबले में कामयाब नहीं करता, इसलिए उन्होंने मासूम और नाबालिग़ बच्चों की एक फ़ौज 1212 ई० में फ़्रांस से भेजी। परन्तु मार्सल्ज़ के बंदरगाह तक पहुँचते-पहुँचते ये बच्चे तितर-बितर हो गए और ख़ुद ईसाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, लूटमार की और दास बनाकर बेच डाला।
बच्चों की सलीबी जंग इस बात का भी सबूत है कि उस ज़माने में यूरोप की क़ौमें मानसिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई थीं।]
उस काल में ईसाइयों की हुकूमत सिर्फ़ यूरोप में थी। सलजूक़ियों के पतन के बाद जर्मनी, फ़्रांस, इटली और यूरोप के अन्य देशों से एक विशाल सेना बैतुल मक़दिस रवाना हुई। पहली सेना तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई और उसे रूम के सलजूक़ी तुर्कों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन जब दूसरी सेना रवाना हुई तो मुसलमान आपस के मतभेदों के कारण ईसाइयों का मुक़ाबला नहीं कर सके। ईसाइयों ने एशिया-ए-कोचक और शाम का सम्पूर्ण समुद्र तटीय क्षेत्र जीतकर 492 हि०/1099 ई० में बैतुल मक़दिस भी फ़तह कर लिया। यहाँ ईसाई फ़ौजियों ने मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का क़त्लेआम किया। जिन लोगों ने मस्जिदे अक़सा में पनाह ली, उन्हें भी नहीं छोड़ा। कहते हैं इस क़त्लेआम में सत्तर हज़ार मुसलमान शहीद हुए। यूरोप के इन ईसाइयों ने अब पूरे फ़िलस्तीन और शाम के समुद्र तटीय क्षेत्र पर अपनी हुकूमत क़ायम कर ली।
शाम के भीतरी शहर हलब, हमात, हिम्स, बालबक और दमिश्क़ पर सलीबी कभी भी क़ाबिज़ न हो सके। मसीहियों ने अपने अधिकृत इलाक़ों में निम्न चार रियासतें क़ायम कर लीं, जो लातीनी रियासतें कहलाती थीं—
1. पहली रियासत 1097 ई० में क़ायम हुई, इसका केन्द्र अर-रुहा (Edessa) था।
2. दूसरी रियासत 1098 ई० में क़ायम हुई, इसका केन्द्र अन्ताकिया था।
3. तीसरी रियासत फ़िलस्तीन की थी जो 1099 ई० में क़ायम हुई, इसका केन्द्र यरुशलम था।
4. चौधी रियासत 1109 ई० में क़ायम हुई और इसका केन्द्र तुराबुलस (Tripolis) था।
इन रियासतों में फ़िलस्तीन की रियासत सबसे बड़ी थी। उसके हुक्मरान की हैसियत शहनशाह के समतुल्य थी और शेष तीन रियासतें औपचारिक तौर पर यरुशलम की अधीनता स्वीकार करती थीं।
सलीबी जंगों के दो बड़े गिरोह थे। एक गिरोह हैकली कहलाता था, इसलिए कि उन्होंने यरुशलम में 'हैकल-सुलैमानी' के निकट रहना शुरू कर दिया था। दूसरा 'हास्पीटलिर्स' कहलाता था। यह हास्पीटल या होस्टल शुरू में मेहमान-ख़ाना था और ये लोग तीर्थयात्रियों की मेहमानदारी करते थे। फिर उन्होंने जंगी गिरोह की हैसियत धारण कर ली।
जब फ़िलस्तीन पर ईसाइयों का क़ब्ज़ा हो गया तो इस्लामी दुनिया में क्षोभ एवं दुख की लहर दौड़ गई। फ़िलस्तीन इस्लामी दुनिया का दिल है। मानचित्र पर देखें तो पता चलेगा कि हालाँकि फ़िलस्तीन एक छोटा-सा इलाक़ा है लेकिन ऐसी जगह स्थित है कि यदि उसपर ग़ैर-मुस्लिमों का क़ब्ज़ा हो जाए तो इस्लामी दुनिया दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। मिस्र और उत्तरी अफ़्रीक़ा के मुसलमान फिर स्थल मार्ग से अरब, इराक़ और ईरान आदि देशों में आ-जा नहीं सकते। इसके अलावा यरुशलम मुसलमानों के लिए भी बड़ा पवित्र स्थल है, इसी लिए मुसलमान उसे क़िब्ल-ए-अव्वल कहते हैं। हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम), दाऊद (अलैहिस्सलाम), मूसा (अलैहिस्सलाम) और ईसा (अलैहिस्सलाम) इसी भूभाग में पैदा हुए हैं और जिस प्रकार वे ईसाइयों और यहूदियों के पैग़म्बर हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के पैग़म्बर भी हैं। और फिर आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जब मेराज हुई तो वे मस्जिदे अक़सा ही में ठहरे थे और यहाँ से आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे। इन परिस्थितियों में मुसलमानों के लिए यह संभव नहीं था कि वे फ़िलस्तीन पर ईसाइयों का क़ब्ज़ा ख़ामोशी से स्वीकार कर लेते। उन्होंने ईसाइयों का मुक़ाबला करने की कोशिश की। जिन लोगों ने ईसाइयों के मुक़ाबले में नाम पैदा किया उनमें पहला मशहूर शख़्स 'अमादुद्दीन ज़ंगी' (521 हि० से 541 हि०) है। अमादुद्दीन सलजूक़ी हुकूमत की ओर से 'मोसल' शहर का गवर्नर था। जब सलजूक़ी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उसने अपनी सल्तनत बहुत बढ़ा ली और ईसाइयों को कई बार पराजित कर उनकी चार रियासतों में से एक रियासत समाप्त कर दी, जिसका केन्द्र शहर अर्रुहा (Edessa) था जिसे आजकल ओरफ़ा (Orfa) कहा जाता है और यह एशिया-ए-कोचक में स्थित है, लेकिन दुर्भाग्यवश अमादुद्दीन की इस बीच मृत्यु हो गई और वह फ़िलस्तीन तक नहीं पहुँच सका। अमादुद्दीन की सारी उम्र लड़ाइयों में गुज़री। वह रणभूमि का इतना अभ्यस्त हो गया था कि कहा करता था-
"मुझे क़ालीनों से अधिक घोड़े की पीठ पर और गीत-संगीत से अधिक तलवारों की झंकारों में मज़ा आता है।"
अमादुद्दीन की यही बहादुरी थी जिसके कारण उसने अकेले यूरोपीय देशों के संयुक्त मोर्चे का मुक़ाबला किया।
नूरुद्दीन ज़ंगी (541 हि० 1146 ई० से 569 हि० 1173 ई०)
अमादुद्दीन ज़ंगी के बाद उसके लड़के नूरुद्दीन ज़ंगी ने इतिहास में बहुत नाम पैदा किया। उसने ईसाइयों से बैतुल मक़दिस वापस लेने से पहले एक मज़बूत हुकूमत क़ायम करने की कोशिश की और इस मक़सद की प्राप्ति के लिए नूरुद्दीन ने आस-पास की छोटी-छोटी मुसलमान हुकूमतों को समाप्त करके, उन्हें अपनी सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। प्रारंभ में उसकी राजधानी 'हलब' में थी। 549 हि०/1154 ई० में उसने दमिश्क़ पर क़बज़ा करके उसको अपनी राजधानी बनाया। उस काल में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत थी, परन्तु अब वह बिलकुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़िलस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए ईसाई उसपर क़बज़ा करना चाहते थे। यह देख कर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 हि०/1168 ई० में मिस्र पर भी क़बज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का अन्त कर दिया। मिस्र पर क़बज़ा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मक़दिस पर आक्रमण करने की तैयारियाँ प्रारंभ कर दीं। बैतुल मक़दिस की मस्जिदे उमर में रखने के लिए उसने बहुत ही उच्च कोटि का मिम्बर तैयार करवाया। उसकी इच्छा थी कि बैतुल मक़दिस पर फ़तह के बाद इस मिम्बर को अपने हाथ से मस्जिद में रखेगा। परन्तु अल्लाह को यह मंज़ूर नहीं था। नूरुद्दीन अभी आक्रमण की तैयारियाँ ही कर रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई।

चित्र 5 :- मोसल से पूर्व की ओर जानेवाली सड़क पर ज़ाख़ू के मक़ाम पर पक्का पुल ज़ंगी काल की यादगार है — नूरुद्दीन ज़ंगी और उसके जानशीनों का दौर जो अताबुक काल कहलाता है, जनकल्याण के कार्यों के कारण बहुत प्रसिद्ध था।

चित्र 6 :- मोसल की जामा मसजिद का मीनार
इस मसजिद और मीनार को सुलतान नूरुद्दीन ज़ंगी ने 1172 ई० में बनवाया था। यह मीनार नक़्शनिगारी का उत्कृष्ट नमूना समझा जाता है।
नूरुद्दीन की उम्र 58 साल थी और उसने 28 साल हुकूमत की। नूरुद्दीन वीरता में अपने बाप की तरह था। एक बार जंग में उसे दुश्मनों की पंक्तियों में बार-बार घुसते देखकर उसके एक दरबारी क़ुत्बुद्दीन ने कहा—
"ऐ हमारे बादशाह!! अपने आपको इम्तिहान में न डालिए, अगर आप मारे गऐ तो दुश्मन इस देश को जीत लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी।"
नूरुद्दीन ने यह बात सुनी तो उसपर बहुत नाराज़ हुआ और कहा—
"क़ुत्बुद्दीन ज़बान को रोको। तुम अल्लाह के हुज़ूर में ग़ुस्ताख़ी कर रहे हो, मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का रक्षक अल्लाह के सिवा कौन था?"
नूरुद्दीन मात्र एक विजेता ही नहीं था, बल्कि एक दयालु हुक्मरान और कुशल प्रशासक भी था। उसने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया और उसके न्याय के क़िस्से दूर-दूर तक फैल गए।
वह बहुत-साधारण जीवन व्यतीत करता था। बैतुल माल का रुपया कभी अपनी निजी ज़रूरत पर ख़र्च नहीं करता था। माले ग़नीमत से उसने कुछ दुकानें ख़रीद ली थीं। उनके किराए से वह अपना ख़र्च पूरा करता था। उसने अपने लिए बड़े-बड़े महल नहीं बनवाए, बल्कि बैतुलमाल का रुपया मदरसों, अस्पतालों और मुसाफ़िरख़ानों के स्थापित करने और जनकल्याण के दूसरे कामों में ख़र्च करता था। दमिश्क़ में उसने एक शानदार अस्पताल बनवाया था, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं थी। उसमें मरीज़ों को मुफ़्त दवा दी जाती थी और खाने और रहने का ख़र्च भी हुकूमत देती थी। इस सम्बन्ध में इतिहास में एक बड़ा दिलचस्प वाक़िआ दर्ज है।
नूरुद्दीन की मृत्यु के लगभग ढाई सौ साल के बाद एक लेखक दमिश्क़ की सैर करता हुआ उस अस्पताल में भी आया। यहाँ मरीज़ों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने-पीने की चीज़ों को देखकर वह ख़ुद मरीज़ बन गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल के प्रधान चिकित्सक ने उसका चेकअप किया और स्वादिष्ट खाने, गोश्त, मुर्ग़, मिठाईयाँ और फ़ल खाने को बताया। परन्तु चिकित्सक चूँकि असल बीमारी को ताड़ चुका था इसलिए उसने तीन दिन के बाद एक पर्ची लिखकर भेजा कि मेहमान तीन दिन से अधिक नहीं ठहर सकता।
नूरुद्दीन की इन ख़ूबियों और कारनामों के कारण उस काल के एक इतिहासकार इब्ने असीर ने लिखा है—
"मैंने इस्लामी काल के हुक्मरानों से लेकर इस वक़्त तक के तमाम बादशाहों के इतिहास का अध्ययन किया, लेकिन ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अतिरिक्त नूरुद्दीन से अच्छा प्रशासक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा।"
नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज़ टैक्स ख़त्म कर दिए थे। मज़लूम लोगों की शिकायत ख़ुद सुनता और ख़ुद उसकी छानबीन करता था।
एक बार एक व्यक्ति ने ज़मीन या जायदाद के सम्बन्ध में नूरुद्दीन पर दावा दायर किया। अदालत का चपरासी उस समय जबकि वह चौगान खेल रहा था, पहुँचा। सुलतान तुरन्त उसके साथ क़ाज़ी की अदालत में पहुंचा और क़ाज़ी से कहा कि इस समय प्रतिवादी की हैसियत से आया हूँ, इसलिए मेरे साथ वही व्यवहार कीजिए जो एक आम प्रतिवादी के साथ किया जाता है। क़ाज़ी ने वादी के बराबर बैठाकर दोनों पक्ष के बयानात और गवाहियाँ सुनीं। जायदाद नूरुद्दीन की साबित हुई और मुक़द्दमा ख़ारिज हो गया।
नूरुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन के किसी फ़ौजी ने एक व्यक्ति पर कुछ ज़्यादती की। मज़लूम व्यक्ति ने सलाहुद्दीन से फ़रियाद की, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। वह मायूस होकर रोता-पीटता नूरुद्दीन के मज़ार पर पहुंचा और यह कहता जाता था— "नूरुद्दीन आज तुम्हारा न्याय कहाँ है। जिस ज़ुल्म के हम लोग शिकार हैं, यदि तुम देख सकते तो तुम्हें हमारी हालत पर रहम आ जाता।" सलाहुद्दीन उस समय दमिश्क़ में मौजूद था, उसे ख़बर हुई तो तुरन्त उस व्यक्ति को बुलाकर उसकी शिकायत दूर की और रुपया-पैसा देकर उसके साथ प्रेम प्रकट किया। इसपर वह व्यक्ति और अधिक रोने लगा। सलाहुद्दीन ने पूछा, "अब क्यों रोते हो?" उसने कहा, "उस बादशाह के दुख में रोता हूँ जिसकी मौत के बाद भी इनसाफ़ क़ायम है।"
सलाहुद्दीन ने कहा, "सच कहते हो, हममें जो कुछ भी न्याय एवं इनसाफ़ है उसी नूरुद्दीन के कारण है।"
एक बार नूरुद्दीन की बीवी ने कहला भेजा कि सुल्तान उसे घर के ख़र्च के लिए जो रक़म देता है वह पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ वृद्धि की जाए। सुल्तान ने इनकार कर दिया और कहलवा दिया कि इससे ज़्यादा कहाँ से लाकर दूँ। यदि वे समझती हैं कि मेरे पास जो माल है वह मेरा अपना है तो यह ग़लत है। यह जनता का माल है और उन्हीं के फ़ायदे के लिए है। मैं मात्र इसका ख़ज़ानची और रखवाला हूँ।
नूरुद्दीन ने शराबनोशी और शराब के धंधे को रोक दिया था। उसने शरीअ़त की ख़ुद पाबंदी की और अपने साथियों को भी इसका पाबंद बनाया। उन्हें देखकर दूसरों ने अनुसरण किया जिसके कारण इस्लाम पर अमल करने का लोगों में ऐसा जज़्बा पैदा हो गया कि लोग शरीअ़त के विपरीत कामों की चर्चा से भी शर्माने लगे।
सलाहुद्दीन (569 हि०/1173 ई० से 589 हि० 1193 ई०)
सलीबी जंगों में सबसे अधिक प्रसिद्धी जिस व्यक्ति को प्राप्त हुई, वह सुल्तान सलाहुद्दीन विजेता बैतुल-मक़दिस है। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्ल से कुर्द था और कुर्दिस्तान के उस भाग में पैदा हुआ था जो इराक़ में सम्मिलित है। प्रारम्भ में वह सुल्तान नूरुद्दीन के यहाँ एक फ़ौजी अफ़सर था। मिस्र को जिस फ़ौज ने फ़तह किया था उसमें सलाहुद्दीन मौजूद था और उस फ़ौज का सिपहसालार उसका चचा शेर कोह था। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन 564 हि०/1168 ई० में मिस्र का हाकिम (गवर्नर) नियुक्त कर दिया गया। उसी काल में यानी 569 हि०/1173 ई० में उसने यमन भी जीत लिया। नूरुद्दीन की मृत्यु के बाद चूँकि उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सलाहुद्दीन सम्पूर्ण सल्तनत पर क़ाबिज़ हो गया।
सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन से भी बाज़ी ले गया। उसमें जिहाद का जोश कूट-कूटकर भरा हुआ था और बैतुल मक़दिस की फ़तह उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। फ़िलस्तीन अब हर ओर से घिर गया था, इसलिए अब उसने बैतुल मक़दिस का रुख़ किया। हित्तीन के मैदान में ईसाइयों से भीषण युद्ध हुआ। ईसाइयों को पराजय का मुँह देखना पड़ा। उनके कई हज़ार आदमी युद्ध में काम आए और कई हज़ार गिरफ़्तार कर लिए गए। सलाहुद्दीन ने आगे बढ़कर आसानी से बैतुल मक़दिस पर क़बज़ा कर लिया और सम्पूर्ण फ़िलस्तीन से मसीही हुकूमत का अन्त हो गया। मस्जिदे अक़्सा में दाख़िल होकर सलाहुद्दीन ने वह मिम्बर जिसे नूरुद्दीन ने बनवाया था, अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस प्रकार नूरुद्दीन की इच्छा सलाहुद्दीन के हाथों पूरी हुई।
सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दिस में दाख़िल होकर वैसा कोई अत्याचार नहीं किया जैसा इस शहर पर क़ब्ज़ा करते समय यूरोप की मसीही फ़ौजों ने मुसलमानों पर किया था। सलाहुद्दीन एक आदर्श विजेता के रूप में बैतुल-मक़दिस में दाख़िल हुआ। उसने फ़िदया लेकर ईसाइयों को अमान दे दी। जो निर्धन फ़िदया नहीं दे सके, उनके फ़िदया की रक़म सलाहुद्दीन और उसके भाई मलिक आदिल ने ख़ुद चुकाई।
बैतुल-मक़दिस पर क़बज़े के साथ यरुशलम की वह मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़िलस्तीन में 1099 ई० में क़ायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फ़िलस्तीन मुसलमानों के क़बज़े में आ गया और ईसाइयों के पास केवल समुद्र तटीय क्षेत्र बचा।
जब बैतुल मक़दिस पर क़बज़े की ख़बर यूरोप पहुँची तो सम्पूर्ण यूरोप में कुहराम मच गया। हर ओर लड़ाई की तैयारियाँ प्रारंभ हो गईं। जर्मनी, इटली, फ़्रांस और इंगलैण्ड से फ़ौजें फ़िलस्तीन रवाना होने लगीं। इंगलैण्ड का बादशाह रिचर्ड जो अपनी वीरता के कारण शेरदिल प्रसिद्ध था और फ़्रांस का बादशाह फ़िलिप अपनी-अपनी फ़ौजें लेकर फ़िलस्तीन पहुँचे। यूरोप की इस संयुक्त सेना का, जिसकी तादाद छः लाख थी, सलाहुद्दीन ने तीन साल तक अकेले मुक़ाबला किया, परन्तु ईसाई बैतुल मक़दिस लेने में सफल नहीं हो सके और सुल्तान से सुलह करके ख़ाली हाथ चले गए। यह लड़ाई तीसरी सलीबी जंग कहलाती है। इसमें सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली हुक्मरान है।
सलाहुद्दीन का जीवन-चरित्र
सलाहुद्दीन बड़ा वीर और दयालु था। लड़ाइयों में उसने ईसाइयों के साथ इतने अच्छे सुलूक किए कि ईसाई आज भी उसकी इज़्ज़त करते हैं।
उसे जिहाद का इतना शौक़ था कि एक बार उसके शरीर के नीचे के आधे धड़ में फ़ोड़े हो गए थे जिनके कारण वह बैठ कर खाना भी नहीं खा सकता था, इस हालत में भी उसकी जिहाद की सरगर्मी में कोई अन्तर नहीं आया। सुबह से ज़ुह्र तक और अस्र से मग़रिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहता। उसे ख़ुद आश्चर्य होता था और कहा करता था कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तक्लीफ़ जाती रहती है और उससे उतरने पर पुनः तक्लीफ़ शुरू हो जाती है।
मसीहियों से समझौता हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने ईसाइयों को बैतुल मक़दिस के दर्शन की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने पर यूरोप के ये दर्शनार्थी जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, दर्शन के लिए इतनी अधिक संख्या में टूट पड़े कि शाह रिचर्ड को इसकी व्यवस्था करना कठिन हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वह उसकी लिखित अनुमति के बिना किसी को बैतुल-मक़दिस में दाख़िल न होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया, “दर्शनार्थी लम्बी यात्राएँ करके दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें रोकना उचित नहीं।"
सुल्तान ने न केवल यह कि उन दर्शनार्थियों को हर प्रकार की आज़ादी दी, बल्कि अपनी ओर से लाखों दर्शनार्थियों के आतिथ्य, सुविधा एवं आराम की व्यवस्था की। वह उनसे मिलकर बातें करता और उनसे प्रेम प्रकट करता।
एक बार उसके कुछ सिपाही एक ईसाई औरत के बच्चे को उठा लाए। औरत बड़ी परेशान हुई। लोगों ने उससे कहा कि तुम सलाहुद्दीन के पास चली जाओ, वह बहुत अच्छा बादशाह है, वह तुम्हारे साथ इनसाफ़ करेगा। औरत रोती हुई बादशाह के पास पहुँची और सारा क़िस्सा सुनाया। उस औरत को रोते देखकर वह भी रो दिया और फ़ौज में बच्चे को तलाश कराकर उसके हवाले कर दिया। सलाहुद्दीन ने ग़ैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक किया, वह इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार था और वह इसका सुबूत है कि इस्लामी हुकूमत में ग़ैर मुस्लिमों के अधिकार भी उसी प्रकार सुरक्षित हैं, जिस प्रकार मुसलमानों के।
नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन का जीवन भी बहुत सरल था। उसने रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली-सा मकान होता था।
जनकल्याण के काम
क़ाहिरा पर क़बज़ा करने के बाद जब सलाहुद्दीन ने फ़ातिमी हुक्मरानों के महलों का जायजा लिया तो वहाँ अनगिनत जवाहरात और सोने-चाँदी के बर्तन जमा थे। सलाहुद्दीन ने ये सारी चीज़ें अपने कबज़े में लाने के बदले बैतुलमाल में जमा करा दीं। लौंडियों को या तो आज़ाद कर दिया या अमीरों में बाँट दिया। इसी प्रकार महलों को आम इस्तेमाल में लाया। एक महल में उसने एक विशाल ख़ानक़ाह क़ायम कर दी।
फ़ातिमियों के काल में मदरसे क़ायम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन के ज़माने में ख़ूब मदरसे और अस्पताल क़ायम हुए, परन्तु मिस्र अब तक वंचित था। सलाहुद्दीन ने यहाँ बहुलता से मदरसे और अस्पताल खुलवाए। इन मदरसों में छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होती थी।
क़ाहिरा में उसने जो अस्पताल बनवाया था, वह सबसे शानदार था। उसके सम्बन्ध में उस काल का एक पर्यटक इब्ने ज़ुबैर लिखता है—
"यह बहुत ही सुन्दर और शानदार महल लगता है। इसमें दवाओं का बहुत बड़ा भण्डार है। मरीज़ों के बहुत-से कमरे हैं। पलंग और बिस्तरों की पूरी व्यवस्था है। कर्मचारी दोनों समय सुबह-शाम मरीज़ों को देखते और उनकी दवा एवं ख़ुराक आदि की व्यवस्था करते हैं। उससे लगा हुआ औरतों का अस्पताल है। उनके इलाज के लिए औरतें नियुक्त हैं। अस्पताल से लगा हुआ एक पागलख़ाना है जिसकी खिड़कियों में जालियाँ लगी हुई हैं। उन पागलों का इलाज और देखभाल मरीज़ों की तरह होती है। सुल्तान हमेशा हालात की छानबीन और मरीज़ों के इलाज एवं निगरानी की ताकीद करता रहता है।"
सलाहुद्दीन के काल में जिस बहुलता से मदरसे, अस्पताल और मुसाफ़िरख़ाने बनाए गए, उनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। उसके समय में हुकूमत की पूरी आमदनी जनकल्याण के कामों पर ख़र्च होती थी। इस मामले में उसका काल निज़ामुल-मुल्क तूसी और नूरुद्दीन ज़ंगी से भी आगे बढ़ गया।
सुल्तान की मिसाल को देखकर उस काल के अमीरों और औरतों तक ने मदरसे स्थापित करने शुरू कर दिए।
सलाहुद्दीन ग़ौरी हुक्मरान शहाबुद्दीन और मराकशी हुक्मरान याक़ूब अल-मंसूर का समकालीन था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये तीनों हुक्मरान अपने समय में दुनिया के महान हुकमरानों में से थे। सलाहुद्दीन का 589 हि०/1193 ई० में इंतिक़ाल हुआ। उसने कुल बीस वर्ष हुकूमत की। इतिहासकार इब्ने ख़लकान ने, जो थोड़े समय बाद हुआ है, अपनी किताब में लिखा है—
"उसकी मौत का दिन इतना कष्टदायक था कि इतना कष्टदायक दिन इस्लाम और मुसलमानों पर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन [प्रथम चार ख़लीफ़ा जिनके सत्य-पथ पर होने में कोई संदेह नहीं। ये चार ख़लीफ़ा हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं।] की मौत के बाद कभी नहीं आया।"
वर्तमान काल के एक अंग्रेज़ इतिहासकार लीन पोल (1908-1991 ई०) ने भी सुल्तान की बड़ी प्रशंसा की है, वह लिखता है—
“उसके समकालीन बादशाहों और उसमें एक आश्चर्यजनक अन्तर था। बादशाहों ने अपने पद और धन के कारण प्रतिष्ठा पाई और उसने प्रजा से प्रेम और उनके मामलात में रुचि लेकर लोकप्रियता की दौलत कमाई।"
सलाहुद्दीन ने जो हुकूमत क़ायम की थी वह उसके बाप नज्मुद्दीन अय्यूब के नाम पर 'अय्यूबी' कहलाती है।
सलाहुद्दीन हालाँकि एक बुद्धिमान और योग्य हुक्मरान था, परन्तु वह ख़ुद को पारंपरिक मान्यताओं से आज़ाद न कर सका। ख़िलाफ़त की मूल अवधारणा को अब मुस्लिम समाज इस हद तक भुला चुका था कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन जैसे हुक्मरान भी मुलूकियत के अंदाज़ में सोचते थे। उत्तराधिकारी के मामले में सलाहुद्दीन ने भी वही ग़लती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सलजूक़ियों के बाद से सभी हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उसने उस समय के ग़लत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत अपने तीन लड़कों में बाँट दी। परिणाम यह हुआ कि यह शक्तिशाली सल्तनत बँटकर कमज़ोर पड़ गई। फिर अय्यूबी ख़ानदान के कुछ अयोग्य हुक्मरान जिनमें सलाहुददीन का भाई मलिक आदिल और उसका लड़का मलिक कामिल उल्लेखनीय हैं, मिस्र, शाम, हिजाज़ और यमन को तक़रीबन साठ साल तक संगठित किए रखा। 648 हि०/1250 ई० में अय्यूबी ख़ानदान की हुकूमत समाप्त हो गई। उसकी जगह तुर्क ग़ुलामों की हुकूमत क़ायम हुई जो 'ममलूक हुकूमत' कहलाती है।
इस काल की एक विशेष बात यह है कि मलिक कामिल ने 1229 ई० में बैतुल-मक़दिस बिना किसी लड़ाई के एक दोस्ताना समझौते के ज़रीये ईसाइयों के हवाले कर दिया। यह एक बड़ा अफ़सोसनाक समझौता था। मलिक कामिल ने सक़लिया के हुक्मरान फ़्रेडरिक से यह समझौता मात्र इसलिए किया था कि वह अय्यूबी ख़ानदान के दूसरे शहज़ादों के मुक़ाबले में जो मलिक कामिल के प्रतिद्वंद्वी थे, उसकी मदद करेगा। इस मदद के बदले में मलिक कामिल ने बैतुल मक़दिस और समुद्र तट का कुछ इलाक़ा फ़्रेडरिक के हवाले कर दिया। आम मुसलमान इस शर्मनाक समझौते पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने बैतुल मक़दिस को पुनः प्राप्त करने का आन्दोलन शुरू किया और 1244 ई० में यानी पंद्रह साल बाद मुसलमानों ने यह शहर ईसाइयों से पुन: छीन लिया।
अय्यूबी हुक्मरान ज्ञान एवं साहित्य में भी बड़े सरपरस्त थे और उनकी सरपरस्ती के कारण अन्दलुस (स्पेन) से कई विद्वान मिस्र और शाम आ गए। उनमें एक मशहूर आलिम और सूफ़ी इब्ने-अरबी (560 हि०/1165 ई० से 638 हि०/1240 ई०) हैं। दूसरे इब्ने-बैतार (646 हि०/1248 ई०) हैं जो अपने काल के वनस्पति विज्ञान के सबसे बड़े माहिर थे। उन्होंने कई सौ ऐसी नई जड़ी-बूटियों की खोज की जो इलाज में काम आती हैं। ये लोग अन्दलुस और उत्तरी अफ़्रीक़ा में मुवह्हिदीन की हुकूमत के पतन के बाद मिस्र और शाम आ गए थे।
इब्ने-जुबैर (540 हि०/1145 ई० से 614 हि०/1217 ई०)
नासिर ख़ुसरो ने फ़ातिमी हुकूमत के काल में मिस्र एवं शाम का जो हाल लिखा है, वह हम पढ़ चुके हैं। नासिर ख़ुसरो के सौ साल बाद एक और प्रसिद्ध पर्यटक इब्ने जुबैर ने मिस्र, शाम और इराक़ की सैर की। नासिर ख़ुसरो इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग यानी ख़ुरासान से आया था, परन्तु इब्ने जुबैर उसके ठीक विपरीत इस्लामी दुनिया के पश्चिमी भाग यानि अन्दलुस (स्पेन) से आया था। यह ज़माना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था और मिस्र और शाम ने नूरुद्दीन एवं सलाहुद्दीन के स्वर्णकाल में बहुत तरक़्क़ी कर ली थी। यह तरक़्क़ी विशेष कर मदरसों और अस्पतालों के क्षेत्र में हुई थी। छठी हिजरी शताब्दी का यह ज़माना जिसमें इब्ने जुबैर ने इस्लामी दुनिया के एक बड़े भूभाग की सैर की, चूंकि अरबों के सांस्कृतिक उन्नति का अन्तिम ज़माना है, इसलिए हम यहाँ इब्ने जुबैर के यात्रा वृतांत का संक्षिप्त हाल लिखते हैं। इसे पढ़कर अंदाज़ा होगा कि फ़ातिमियों के बाद मिस्र एवं शाम के जन-जीवन में बहुत अन्तर आ गया था और मुसलमान अपने सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष पर पहुँच गए थे।
इब्ने जुबैर अन्दलुस से चलने के बाद सबसे पहले स्कंदरिया आया जो वर्तमान काल की तरह उस समय भी मिस्र की सबसे बड़ी बंदरगाह था। उसके सम्बन्ध में वह लिखता है—
"हमने अब तक कोई ऐसा शहर नहीं देखा जिसकी सड़कें स्कंदरिया से ज़्यादा चौड़ी हों और जिसकी इमारतें स्कंदरिया की इमारतों से ज़्यादा बुलंद हों या जो उसकी तरह प्राचीन और सुन्दर हों। यहाँ के बाज़ार शानदार हैं और शहर के मुख्य स्थलों में से एक वहाँ के मदरसे और अस्पताल हैं।"
“स्कंदरिया में छात्रों के आवास और उनकी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था है। छात्रों को उनकी अन्य ज़रूरतों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। सुल्तान ने दूर दराज़ से आनेवाले यात्रियों के नहाने और सफ़ाई के लिए स्नानगृहों तक की व्यवस्था की है और उनके इलाज के लिए अस्पताल क़ायम किया है और उन्हें देखने के लिए चिकित्सक नियुक्त हैं।"
“शहर के वासियों की एक विशेषता यह है कि यहाँ के लोग दिन के अलावा रात को भी काम करते हैं। दूसरे शहरों के मुक़ाबले में यहाँ मस्जिदों की तादाद ज़्यादा है। कुछ लोगों के अनुसार उनकी तादाद बारह हज़ार तक है। सुल्तान की ओर से हर इमाम को वज़ीफ़ा मिलता है।"
स्कंदरिया के बाद इब्ने जुबैर क़ाहिरा पहुँचा जो दमिश्क़ के बाद सलाहुद्दीन की दूसरी राजधानी थी। यहाँ इब्ने जुबैर क़ाहिरा के बड़े अस्पताल से, जिसे हाल ही में बनवाया गया था, बहुत प्रभावित हुआ। वह लिखता है—
"क़ाहिरा का अस्पताल उल्लेखनीय है। यह अपनी विशालता और सुन्दरता में महल जैसा है। इसके कमरों में बीमारों के लिए बिस्तर बिछे रहते हैं। नौकर सुबह व शाम उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें ख़ुराक और दवा लाकर देते हैं। उसके सामने औरतों का एक अस्पताल है। वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है। उन दोनों अस्पतालों से मिला हुआ एक तीसरा अस्पताल है जो पागलों के लिए विशिष्ट है। उसके कमरों की खिड़कियों में लोहे की सलाख़ें लगी हुई हैं। फ़िस्तात में भी इस नमूने का एक अस्पताल है।"
“क़ाहिरा में कोई मस्जिद, मक़बरा या मदरसा ऐसा नहीं है जो सुल्तान की दानशीलता से वंचित हो। यहाँ सुल्तान ने एक मदरसा बनवाया है। जहाँ सिर्फ़ अनाथ और ग़रीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है।"
"सुल्तान का एक बड़ा कारनामा उन चुंगियों को ख़त्म करना है जो फ़ातिमियों के ज़माने में हाजियों पर लगाई गई थीं। सुल्तान ने हाजियों के लिए ख़ुराक और सफ़र के सामानों की व्यवस्था भी कर दी है।
".........सुल्तान का इनसाफ़ ऐसा है — सड़कों को उसने ऐसा सुरक्षित बना दिया कि लोग रात को भी बिना भय अपने काम कर सकते हैं।"
मिस्र से इब्ने जुबैर हज करने के लिए मदीना होता हुआ मक्का गया। फिर वहाँ से बग़दाद आया और इराक़ के शहरों की सैर करता हुआ शाम आया। बग़दाद और इराक़ के दूसरे शहरों का उसने जो हाल लिखा है वह हम दूसरे किसी अध्याय में लिखेंगे। यह अध्याय चूँकि अय्यूबी काल से संबंधित है इसलिए यहाँ हम सिर्फ़ शाम के शहरों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे।
हलब की इब्ने जुबैर ने बड़ी प्रशंसा की है। वह लिखता है—
"शहर अति सुन्दर है। बड़े-बड़े बाज़ार हैं जो एक-दूसरे से लगे हुए हैं। जामा मस्जिद अति सुन्दर है। मस्जिद के पश्चिम में एक मदरसा है जो सुन्दरता और कारीगरी में मस्जिद ही की तरह है। इस मदरसे के अलावा शहर में चार-पाँच दूसरे मदरसे भी हैं। शहर में एक अस्पताल भी है।
.....हलब शानो-शौकत में ऐसा है कि ख़लीफ़ा का मुख्यालय बनाए जाने योग्य है। यह दुनिया के उन शहरों में से एक है जो अपनी मिसाल आप हैं और जिसकी प्रशंसा करने के लिए समय चाहिए।"
राजधानी दमिश्क़ के सम्बन्ध में लिखता है—
"शहर के आस-पास का इलाक़ा बहुत विस्तृत है, परन्तु ख़ुद शहर बहुत बड़ा नहीं है। सड़कें सँकरी और अन्धकारपूर्ण हैं। घर मिट्टी और सरकंडे के हैं और तीन-तीन मंज़िले हैं। दमिश्क़ दुनिया का सबसे घनी आबादीवाला शहर है और इसकी आबादी तीन शहरों के बराबर है। दमिश्क़ की सुन्दरता उसके बाहरी भाग में है, भीतरी भाग में नहीं।"
“शहर में बीस मदरसे और दो अस्पताल हैं। एक पुराना और एक नया...। इन अस्पतालों में पागलों के इलाज की व्यवस्था भी है। ये अस्पताल और मदरसे इस्लामी दुनिया के लिए गर्व की वस्तु हैं। यहाँ एक अति सुन्दर मदरसा नूरुद्दीन का है जिसमें उसका मज़ार है। यह एक शानदार महल है। इसमें पानी एक छतदार नहर से आता है। पहले फ़व्वारा चलता है और फिर पानी एक बड़े हौज़ में, जो इमारत के बीच में है, गिर जाता है। यह दृश्य बहुत ही दिलकश है।"
“इस शहर में यात्रियों के लिए अनगिनत सुविधाएँ हैं। विशेषकर उनके लिए जो क़ुरआन हिफ़्ज़ करें या इल्म हासिल करें। पूरब के सभी शहर इसी प्रकार के हैं, लेकिन यह शहर ज़्यादा आबाद और दौलतमंद है। पश्चिम का हर नव-युवक जो ख़ुशहाली का इच्छुक है, यदि वह शिक्षा प्राप्ति के लिए अपना देश छोड़कर इस भूभाग में आ जाए तो उसे तरह-तरह की सहायता मिलेगी। ......सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वह रोज़गार से बेफ़िक्र हो जाएगा।"
"दमिश्क़ में सुल्तान का क़िला और शहर के बाहर घुड़दौड़ [इस्लामी इतिहास में घुड़दौड़ का रिवाज ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय से ही हो गया था, लेकिन यह घुड़दौड़ आजकल की घुड़दौड़ से, जिसे 'रेस' कहा जाता है, भिन्न होते थे। आजकल घोड़े जुआ खेलने के लिए दौड़ाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम में जुआ खेलना चूँकि हराम है इसलिए मुसलमान अपने उत्थान काल में केवल मुक़ाबले, खेल-कूद और मनोरंजन के लिए घोड़े दौड़ाते थे, जुआ खेलने के लिए शर्त नहीं लगाते थे।] के दो मैदान हैं। ये बड़े दर्शनीय स्थल हैं। सुल्तान हर शाम को यहाँ आता है। तीरंदाज़ी का अभ्यास करता है। घोड़े दौड़ाता है और चौगान (पोलो) खेलता है।"
प्रायः यह समझा जाता कि फ़लश के पाख़ाने और स्नानगृह यूरोप की खोज हैं। परन्तु इब्ने जुबैर के यात्रा-वृत्तांत से मालूम होता है कि दमिश्क़ में ऐसे पाख़ाने और स्नानगृह आम थे। वह लिखता है—
“दमिश्क़ और उसके आस-पास के इलाक़े में एक सौ स्नानगृह और चालीस पवित्र-गृह हैं। उन सबमें पानी बहता रहता है।"
अका और सौर के सम्बन्ध में जिन पर उस काल में यूरोपवालों का क़ब्ज़ा था वह लिखता है :-
“अका और सौर के गिर्द बाग़ीचे नहीं हैं। अका गंदा है और सौर उसके मुक़ाबले में कुछ साफ़ है।"
डेढ़ सौ साल पहले जब नासिर ख़ुसरो यहाँ आया था, उस समय ये दोनों शहर मुसलमानों के क़ब्ज़े में थे और अपनी सफ़ाई और सुन्दरता में प्रसिद्ध थे, परन्तु यूरोपवालों के क़ब्ज़े के बाद इन शहरों में गंदगी फैल गई।
इसका कारण यह था कि मुसलमान अपने उन्नति काल में ज्ञान एवं सफ़ाई के अलमबरदार थे और यूरोपवाले अज्ञानता और गंदगी में घिरे हुए थे।
अय्यूबी सल्तनत
569 हि०/1174 ई० से 648 हि०/1250 ई०
1. सलाहुद्दीन - 569 हि०/1174 ई० से 589 हि०/1193ई०
2. मलिक अल-अज़ीज़ - 589 हि०/1193 ई० से 595 हि०/1198 ई०
3. मलिक अल-आदिल - 595 हि०/1198 ई० से 615 हि०/1218 ई०
4. मलिक अल-कामिल - 615 हि०/1218 ई० से 635 हि०/1238 ई०
5. मलिक अल-आदिल द्वितीय - 635 हि०/1238 ई० से 637 हि०/1240 ई०
6. मलिक अस्सालेह - 637 हि०/1240 ई० से 647 हि०/1249 ई०
7. तोरान शाह - 647 हि०/1249 ई० से 648 हि०/1250 ई०
हित्तीन की जंग और बैतुल मक़दिस पर विजय - 583 हि०/1187 ई०
तीसरी सलीबी जंग - 585 हि०/1189 ई० से 588 हि०/1192 ई०
अध्याय-18
शहरों की दुल्हन – क़ुरतुबा
पिछले पृष्ठों में जिन हुकूमतों के इतिहास का उल्लेख किया गया है ये सब वे हुकूमतें थीं जो अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन के बाद उन इलाक़ों में क़ायम हुईं जो पहले अब्बासी ख़िलाफ़त की सीमाओं के अन्तर्गत थीं। अब तक अन्दलुस (स्पेन) की इस्लामी हुकूमत का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यह मुल्क अब्बासियों के क़बज़े में कभी नहीं आया और उनकी ख़िलाफ़त क़ायम होने के बाद यहाँ बनी उमैया के ख़ानदान के एक व्यक्ति अब्दुर्रहमान ने अपनी आज़ाद हुकूमत क़ायम कर ली थी।
अब्दुर्रहमान अद-दाख़िल
(138 हि०/756 ई० से 172 हि०/788 ई०)
अब्दुर्रहमान बनी उमैया के प्रसिद्ध ख़लीफ़ा हिशाम का पोता था। उसने किसी प्रकार अपनी जान बचाई। किस प्रकार शाम (सीरिया) से अन्दलुस पहुँचा और कई साल तक कैसी-कैसी मुसीबतें झेलीं, उसके संस्मरण बड़े दिलचस्प और ज्ञानवर्धक हैं। उन संस्मरणों को पढ़कर मालूम होता है कि यदि आदमी किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर ले और हर प्रकार की कठिनाइयों का साहस के साथ मुक़ाबला करे तो वह दुनिया में बड़े से बड़े काम भी कर सकता है।
बनी अब्बास जब बनी उमैया की राजधानी दमिश्क़ पर क़ाबिज़ हो गए तो उन्होंने बनी उमैया के शाही ख़ानदान के लोगों को क़त्ल करना शुरू कर दिया। अदुर्रहमान की उम्र उस समय 19 साल थी। वह फ़ुरात नदी के किनारे एक गाँव में, जो घने जंगल के अन्दर था, अपने घरवालों के साथ छुप गया। परन्तु अब्बासी सेना के सवार यहाँ भी पहुँच गए। अब्दुर्रहमान ने अपनी बहन और एक बच्चे को अपने ग़ुलाम बदर के सुपुर्द किया और ख़ुद मकान के पिछले दरवाज़े से निकल गया। उसका तेरह वर्षीय भाई भी उसके साथ था। सवारों ने उन्हें देख लिया तो ये दोनों फ़ुरात नदी के किनारे लगे हुए घने जंगल में घुस गए। आगे-आगे दोनों भाई भागते जा रहे थे और पीछे दुश्मन के सवार उनका पीछा कर रहे थे। अब ये दोनों नदी के किनारे पुरानी क़ब्रों के अन्दर घुस गए। सवार जब यहाँ पहुँचे तो दोनों निकल भागे और नदी में कूद पड़े। सवारों ने उन्हें आवाज़ दी— "वापस आ जाओ, जान की अमान है (जीवन की सुरक्षा का वचन देते हैं)।”
परन्तु दोनों भाई तैरते गए। पर जब बीच नदी में पहुँचे तो अब्दुर्रहमान का छोटा भाई थक गया। अब्दुर्रहमान ने उसका हौसला बढ़ाया और अपनी ओर बुलाता रहा। परन्तु वह दुश्मन की बातों में आ गया और धीरे-धीरे तैरकर लौट गया। सवारों ने पकड़ते ही उसे क़त्ल कर दिया।
अब्दुर्रहमान यहाँ से फ़िलस्तीन और मिस्र होता हुआ अफ़्रीक़ा पहुँचा। अफ़्रीक़ा में वह लगभग पाँच-छः साल रहा और एक जगह से दूसरी जगह छिपता रहा। इस बीच अन्दलुस में उसके समर्थक पैदा हो गए और अब्दुर्रहमान उनकी मदद से समुद्र पारकर अन्दलुस पहुँच गया और उस मुल्क में एक आज़ाद हुकूमत की बुनियाद डाल दी जो ढाई सौ साल से अधिक अवधि तक क़ायम रही। अन्दलुस में हुकूमत क़ायम हो जाने के बाद अब्दुर्रहमान ने अपने बच्चे को अपने पास बुलवा लिया। उसने बहन को भी बुलवाया, परन्तु उसने यह कहकर इंकार कर दिया कि अब वह शाम (सीरिया) में आराम से है, इसलिए अब सफ़र के ख़तरे में पड़ना उचित नहीं समझती। अब्दुर्रहमान की यह बहन अपने भाई को शाम के मेवे अन्दलुस भेजा करती थी। उन मेवों में एक विशेष प्रकार का अनार था जो अन्दलुस में नहीं होता था। अब्दुर्रहमान ने अन्दलुस में अनार और शाम के दूसरे फलों की खेती शुरू कराई, जिसके कारण यह फल अन्दलुस में भी होने लगा। अब्दुर्रहमान ने क़ुरतुबा को राजधानी बनाया और वहाँ एक विशाल मस्जिद बनवाई जो 'जामे क़ुरतुबा' के नाम से प्रसिद्ध है।
अब्दुर्रहमान चूँकि बाहर से आकर अन्दलुस में दाख़िल हुआ था इसलिए इतिहास में उसे अब्दुर्रहमान अद-दाख़िल भी कहा जाता है। उसने लगभग 33 साल हुकूमत की।
अब्दुर्रहमान के काल की एक अहम घटना शार्लमीन के हमले की नाकामी है। बनी उमैया के हालात में हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमान अब्दुर्रहमान अल-ग़ाफ़क़ी के नेतृत्व में फ़्रांस में तोरस तक पहुँच गए थे, परन्तु उसके बाद वे आगे नहीं बढ़ सके और दक्षिणी-पश्चिमी फ़्रांस के अलावा सारा मुल्क मुसलमानों के हाथ से निकल गया था। इसके बाद एक ईसाई राजा शार्लमीन ने जर्मनी, फ़्रांस और मध्य यूरोप के एक बड़े हिस्से पर क़बज़ा करके शक्तिशाली हुकूमत क़ायम कर ली। अब शार्लमीन ने यह कोशिश की कि अन्दलुस से भी मुसलमानों को निकाल दे। अतः 161 हि०/778 ई० में यानी अब्दुर्रहमान प्रथम के काल में एक ज़बरदस्त फ़ौज लेकर अन्दलुस पर आक्रमण किया और सरकस्ता नामक शहर तक घुस आया। परन्तु मुसलमानों ने यहाँ शार्लमीन को बुरी तरह पराजित किया। उसके बड़े-बड़े फ़ौजी सरदार मारे गए और उसे अन्दलुस (Andlus) छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम फ़्रांस पर फिर मुसलमानों का क़बज़ा हो गया।
हिशाम प्रथम (171 हि०/787 ई० से 180 हि० से 796 ई०)
अब्दुर्रहमान अद-दाख़िल के बाद उसका बेटा हिशाम (171 हि० से 180 हि०) गद्दी पर बैठा। हिशाम ने आठ साल हुकूमत की परन्तु इन आठ सालों में जैसी न्याय एवं शान्ति अन्दलुस को प्राप्त हुई वैसी इससे पहले प्राप्त नहीं हुई थी। हिशाम बड़ा ही न्याय-प्रिय हुक्मरान था और वह अपने आचरण एवं व्यवहार में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलता-जुलता था। वह सूबेदारों और हाकिमों (गवर्नरों) पर कड़ी निगरानी रखता था, ताकि वे किसी पर अत्याचार न कर सकें। यदि किसी की शिकायत पहुँचती तो उसे पद से तुरंत हटा देता था। उसने ग़ैर-शरई (शरीअ़त के विरुद्ध) टैक्स समाप्त कर दिए और ज़कात एवं सदक़ा वुसूल करने और उसके वितरण की व्यवस्था की।
हिशाम ने जामे-क़ुरतुबा जिसका निर्माण अब्दुर्रहमान के ज़माने में प्रारम्भ हुआ था, पूरा कराया। इसके अतिरिक्त अल-कबीर नदी पर, जो क़ुरतुबा से बहता था, एक पक्का पुल नए सिरे से बनवाया। जब यह पुल बनकर तैयार हो गया तो हिशाम को मालूम हुआ कि क़ुरतुबा के लोगों का ऐसा विचार है कि हिशाम ने यह पुल अपने सैर-शिकार के आवागमन के लिए बनवाया है, तो उसने इस पुल पर से न गुज़रने का प्रण किया और सारी उम्र उस पुल पर से नहीं गुज़रा।
हिशाम रातों को रुपयों की थैलियाँ लेकर निकल जाता और बूढ़ी और परदा वाली औरतों में बाँटता या मस्जिदों में जाकर लोगों में बाँटता। वह मरीज़ों का हाल मालूम करता और जनाज़ों में शामिल होता। अपनी इन ख़ूबियों के कारण वह लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया।
एक बार वह एक अधिकारी के जनाज़े में शामिल होकर वापस आ रहा था। क़ब्रिस्तान के निकट एक घर से एक कुत्ता निकला और उसपर हमला करके उसकी सदरी फाड़ दी। हिशाम ने शहर के हाकिम (गवर्नर) को आदेश दिया कि वह उस कुत्ते के मालिक पर जुर्माना करे। उसने ऐसी जगह पर कुत्ता क्यों पाल रखा है कि जहाँ उससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। परन्तु बाद में हिशाम ने कुत्ते के मालिक का जुर्माना यह कहकर माफ़ कर दिया कि मुझे कपड़े फटने का जितना अफ़सोस हुआ है उससे अधिक उस कुत्ते के मालिक को इसका अफ़सोस हुआ है कि उसके कुत्ते ने उसके बादशाह पर हमला किया।
हिशाम का उत्तराधिकारी हकम (180 हि०/796 ई० से 206 हि०/821 ई०) अपने बाप की तरह योग्य हुक्मरान साबित नहीं हो सका। उसकी कुछ ग़लत आदतों के कारण आलिम और आम जनता उसके विरुद्ध हो गई और अशान्ति फैल गई। हालाँकि हकम ने हंगामों और उपद्रवों को समाप्त कर दिया, परन्तु आन्तरिक अशान्ति से फ़्रांस की हुकूमत ने फ़ायदा उठाया और मुसलमानों की हुकूमत का न केवल फ़्रांस में अन्त कर दिया बल्कि स्पेन में भी बार्सिलोना तक समुद्र तटीय क्षेत्रों पर क़बज़ा कर लिया। मुसलमानों की हुकूमत अन्दलुस में इसके बाद कई सौ साल तक क़ायम रही, परन्तु दक्षिणी-पश्चिमी फ़्रांस और बार्सिलोना के ये क्षेत्र पुनः उनके क़बज़े में कभी नहीं आए। [इस घटना के लगभग एक सौ साल बाद 889 ई० में अरब मुसलमान एक बार फिर फ़्रांस में दाख़िल हुए, परन्तु ये किसी इस्लामी हुकूमत की बाज़ाब्ता फ़ौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि कुछ अरब मुहिमबाज़ों की कोशिश थी जो समुद्री मार्ग से आकर खाड़ी सेन्ट ट्राप्स के रास्ते दक्षिण फ़्रांस में दाख़िल हुए और स्वीटज़रलैण्ड में कान्सटान्स झील तक बढ़े चले गए। उन्होंने जिन शहरों पर क़बज़ा किया उनमें मार्सल्ज़, नेस और ग्रेनोबल उल्लेखनीय हैं। यह क़बज़ा लगभग 86 साल तक क़ायम रहा। मार्सल्ज़ का एक मुहल्ला आज तक अरबों के नाम पर कहलाता है।
इस संदर्भ में एक और घटना उल्लेखनीय है जो इस बात का प्रमाण है कि उस ज़माने में मुसलमान मुहिमबाज़ों ने अपनी सीमित कोशिशों से कैसे हैरतअंगेज़ कारनामे अनजाम दिए। हकम प्रथम के ज़माने में जब क़ुरतुबा में बग़ावत हुई थी तो हुकूमत ने उसे दबाने के बाद कई हज़ार मुसलमानों को देश निकाला दे दिया। इन मुसलमानों की एक जमाअत मराकश के शहर फ़्रांस में आबाद हो गई और दूसरी जमाअत ने पूर्वी रोम सागर में क्रेट द्वीप जीतकर वहाँ अपनी हुकूमत क़ायम कर ली। क्रेट का शहर केनेडिया मुसलमानों का ही बसाया हुआ है। यह अरबी शब्द 'ख़न्दक़' का विकृत रूप है। क्रेट की यह इस्लामी हुकूमत 210 हि०/825 ई० में क़ायम हुई और 350 हि०/961 ई० तक क़ायम रही। यह हुकूमत अब्बासी ख़िलाफ़त को मानती थी।]
हकम प्रथम का उत्तराधिकारी अब्दुर्रहमान द्वितीय (206 हि०/821 ई० से 238 हि०/852 ई०) जिसे अब्दुर्रहमान-अव्वल भी कहते हैं एक योग्य एवं ज्ञानी बादशाह था। उसका काल बहुत हद तक सुख-चैन एवं शान्ति का काल था। उसके काल में अन्दलुस में पहली बार समुद्री बेड़ा तैयार किया गया और अल-कबीर नदी के तट पर अशबीलिया शहर में जहाज़-निर्माण का बहुत बड़ा कारख़ाना क़ायम हुआ।
अब्दुर्रहमान द्वितीय कला-प्रेमी था। उसके काल में इराक़ से एक प्रसिद्ध गायक ज़रयाब क़ुरतबा आया, जिसे अब्दुर्रहमान ने बहुत प्रोत्साहन दिया। ज़रयाब केवल एक माहिर संगीतकार ही नहीं था बल्कि अपने काल का एक बड़ा फ़ैशन विशेषज्ञ भी था। उसके काल में अन्दलुस के सार्वजनिक जीवन में बहुत परिवर्तन आए और नए-नए परिधान और खाने-पीने के तरीक़े खोजे गए। अब्दुर्रहमान द्वितीय अब्बासी हुक्मरान मामून और मुअतसिम का समकालीन था।
अब्दुर्रहमान अन-नासिर (300 हि०/912 ई० से 350 हि०/961 ई०)
अदुर्रहमान द्वितीय के बाद तीन और हुक्मरान क़ुरतुबा की गद्दी पर बैठे, परन्तु उनके समय में केन्द्रीय हुकूमत कमज़ोर हो गई और देश हंगामों एवं झगड़ों की भेंट चढ़ गया। यह स्थिति अब्दुर्रहमान अन-नासिर के सत्तासीन होने तक रही। अन्दलुस के उमवी हुक्मरानों में से अधिक प्रसिद्धि और महानता अब्दुर्रहमान अन-नासिर (300 हि० से 350 हि०) को प्राप्त हुई। नासिर अब्दुर्रहमान नाम का तीसरा बादशाह था, इसलिए उसे अब्दुर्रहमान तृतीय भी कहते हैं। वह 'अब्दुर्रहमान आज़म' के नाम से भी प्रसिद्ध है।
अब्दुर्रहमान नासिर जब गद्दी पर बैठा तो मुल्क की हालत बहुत ख़राब थी। हर ओर बग़ावतें फैली हुई थीं और बादशाह का आदेश क़ुरतबा से बाहर चलना बंद हो गया था। अन-नासिर की उम्र केवल 22 साल थी, परन्तु इसके बावजूद उसने ऐसी दक्षता से हुकूमत की कि दस-पंद्रह साल के अन्दर-अन्दर सारे मुल्क में शान्ति बहाल हो गई। उसने न केवल इस्लामी अन्दलुस में ही शान्ति बहाल की बल्कि उत्तर के पहाड़ों में जो ईसाई रियासतें थीं और जो अन्दलुस की हुकूमत के प्रभाव से आज़ाद थीं, उन्हें भी अपने अधीन कर लिया और उनसे टैक्स वसूलने लगा।
अब्दुर्रहमान आज़म ने सैनिक शक्ति को बहुत बढ़ाया। उसकी फ़ौज की तादाद डेढ़ लाख थी। इसके अतिरिक्त उसने समुद्री शक्ति को भी विकसित किया। अन्दलुस के समुद्री बेड़े में उस समय दो सौ जहाज़ थे और समुद्र तटों पर पचास हज़ार सिपाही हर वक़्त सुरक्षा के लिए मौजूद रहते थे।
अन्दलुस की इस शक्ति और शान को देखकर यूरोप की हुकूमतों ने अब्दुर्रहमान आज़म से सम्बन्ध स्थापित करना चाहा। अतः क़ुस्तनतीनिया की रूमी हुकूमत और फ़्रांस एवं जर्मनी की हुकूमतों ने अपने प्रतिनिधि उसके दरबार में भेजे। अन्दलुस के उमवी हुक्मरान अब तक 'अमीर' कहलाते थे और उन्होंने ख़िलाफ़त का दावा नहीं किया था, परन्तु चौथी शताब्दी (हिजरी) में बग़दाद पर बनी-बुवैह के क़ब्ज़े के बाद अब्बासी ख़लीफ़ा बनी-बुवैह के हुक्मरानों के अधीन हो गए थे। अब्दुर्रहमान आज़म ने जब यह देखा कि ख़िलाफ़त में जान नहीं रही और वह एक शक्तिशाली हुक्मरान बन गया है तो उसने अमीर की उपाधि छोड़कर अपनी ख़िलाफ़त का एलान कर दिया। इसके बाद से वह और उसके उत्तराधिकारी ख़लीफ़ा कहलाने लगे।
अब्दुर्रहमान आज़म केवल एक शक्तिशाली हुक्मरान ही नहीं था, बल्कि वह बड़ा योग्य, न्यायी और प्रजा का ध्यान रखनेवाला बादशाह था। उसके समय में हुकूमत की आमदनी एक करोड़ बीस लाख दीनार वार्षिक थी। उसमें से एक तिहाई रक़म वह फ़ौज पर ख़र्च करता था और शेष रक़म को ज़रूरत के वक़्त काम आने के लिए ख़ज़ाने में जमा कर देता था।
उसके न्याय एवं इनसाफ़ का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि एक बार उसके लड़के ने बग़ावत कर दी। जब वह गिरफ़्तार करके लाया गया तो अब्दुर्रहमान ने उसे मौत की सज़ा दी। इसपर वलीअहद (उत्तराधिकारी) ने अपने भाई को माफ़ कर देने के लिए गिड़गिड़ाकर सिफ़ारिश की। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, "एक बाप की हैसियत से मैं इसकी मौत पर सारी ज़िंदगी आँसू बहाऊँगा, परन्तु मैं बाप के अलावा बादशाह भी हूँ। यदि बाग़ियों के साथ रियायत करुँगा तो सल्तनत टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी।”
इन तमाम ख़ूबियों के बावजूद अब्दुर्रहमान की ज़िन्दगी एक बादशाह की ज़िंदगी थी। हम उसका मुक़ाबला 'ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन' या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से नहीं कर सकते। न वह नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन की तरह था और न ही अपने ख़ानदान के हिशाम की तरह था। उसने अपनी लौंडी ज़ुहरा के लिए क़ुरतुबा के निकट एक बस्ती बसाई जो मदीनतुज़-ज़ुहरा (ज़ुहरा का शहर) कहलाती है। उसपर उसने करोड़ों रुपये ख़र्च किए। उसका निर्माण चालीस साल तक चलता रहा। पच्चीस साल उसकी ज़िन्दगी में और पंद्रह साल उसके बाद। रोज़ाना दस हज़ार मज़दूर काम करते थे। उसमें शाही ख़ानदान के अमीरों के बड़े-बड़े महल और नौकरों के लिए मकान और सरकारी कार्यालय थे। उसमें एक चिड़िया घर भी था जिसमें तरह-तरह के जानवर थे और शहर के लोग यहाँ मनोरंजन (तफ़रीह) के लिए आते थे।
मदीनतुज़-ज़ुहरा के महलों का निर्माण पूरा होने के बाद लोगों ने ख़लीफ़ा को मुबारकबाद दी। जुमा का दिन था। मस्जिद में सब नमाज़ के लिए जमा हुए। क़ाज़ी मुन्ज़िर ने ख़ुतबा पढ़ा और इस ख़ुतबे में अब्दुर्रहमान की इस फ़िज़ूलख़र्ची की निन्दा की और बुरा-भला कहा। क़ाज़ी मुन्ज़िर बड़े साहसी क़ाज़ी थे। वह हक़ बात कहने से कभी नहीं चूकते थे। अब्दुर्रहमान भी एक न्यायप्रिय हुक्मरान था और उसने क़ाज़ी मुन्ज़िर जैसे आदमी को क़ाज़ी इसलिए नियुक्त किया था कि वह न्याय एवं इनसाफ़ से काम लेने में किसी से न डरें। इसलिए उसने क़ाज़ी साहब की बातें बड़े धैर्य और संयम से सुनीं। अपनी ग़लती स्वीकार की और रोने लगा।
अब्दुर्रहमान आज़म के बाद उसका लड़का हकम द्वितीय (350 हि०/961 ई० से 366 हि०/976 ई०) गद्दी पर बैठा। उसने सोलह साल हुकूमत की। वह पढ़ने-लिखने का बहुत शौक़ीन था। उसने शाही पुस्तकालय में चार लाख पुस्तकें एकत्रित की थीं। किताबें नक़ल करने के लिए उसके महल में दस हज़ार लिखनेवाले मौजूद रहते थे। इस्लामी दुनिया के हर हिस्से में हकम के प्रतिनिधि घूमते रहते थे और जब कोई लेखक अपनी किताब पूरी कर लेता, तो उसे बड़ी क़ीमत देकर ख़रीद लेते थे और क़ुरतुबा के शाही पुस्तकालय के लिए भेज देते थे।
मंसूर (366 हि०/976 ई० से 393 हि०/1003 ई०)
अल-हकम के बाद उसका लड़का हिशाम द्वितीय गद्दी पर बैठा, परन्तु उसके काल में अन्दलुस पर जिस व्यक्ति ने हुकूमत की वह अन्दलुस का प्रधानमंत्री मुहम्मद बिन अबी-आमिर था जो मंसूर के नाम से प्रसिद्ध है। मंसूर का सम्बन्ध एक मामूली परिवार से था। उसने क़ुरतुबा में शिक्षा प्राप्त की। मंसूर बचपन से ही बड़े हौसलेवाला था और हुकूमत के सपने देखा करता था। एक बार वह अपने मित्रों के साथ मनोरंजन के लिए एक बाग़ में गया। उसके दोस्त खेल-कूद में व्यस्त हो गए, परन्तु मंसूर एक किनारे पर चुपचाप बैठ गया। जब उसके दोस्तों ने उसे ख़ामोश देखा तो पूछा, “अरे भाई, तुम यह किस चिन्ता में पड़े हुए हो!"
मंसूर ने जवाब दिया, "मैं सोच रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री बन जाऊँगा तो शहर का क़ाज़ी किस व्यक्ति को बनाऊँगा।"
इस जवाब पर सभी लड़के खिलखिलाकर हँस दिए। “मंसूर यदि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो मुझे अमुक पद दे देना” एक लड़के ने कहा। "मंसूर तुम मुझे अमुक पद दे देना” दूसरे लड़के ने कहा। इसी प्रकार तीसरे लड़के ने भी कुछ निवेदन किया, परन्तु चौथे लड़के ने मज़ाक़ उड़ाया और कहा, “मंसूर यदि तुम बादशाह हो जाओ तो मेरा मुँह काला करके गधे पर बैठाकर शहर से बाहर निकाल देना।"
"तुम सबके साथ वही सुलूक किया जाएगा जिसकी तुम लोगों ने इच्छा प्रकट की है।" मंसूर ने जवाब दिया और उसके सभी साथी खिलखिलाकर हँस पड़े।
कोशिश करनेवालों को ख़ुदा कामयाब करता है। मंसूर को भी ख़ुदा ने कामयाब किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह शाही महल के सामने लोगों की अर्ज़ियाँ लिखने का काम करने लगा। उसके बाद ख़लीफ़ा अल-हकम के बेटे का प्रशिक्षक नियुक्त हुआ। उसके बाद शहर का कोतवाल बना। फिर अफ़्रीक़ा के अभियान का लीडर बनाकर भेजा गया। इस अभियान की सफलता के बाद वह फ़ौज में लोकप्रिय हो गया और सिपाही उसपर जान छिड़कने लगे। और जब ख़लीफ़ा का इन्तिक़ाल हुआ तो वह हाजिब (निगहबान) बन गया। अन्दलुस में चूँकि हाजिब की ज़िम्मेदारी वही होती थी जो पूर्वी देशों में प्रधानमंत्री की होती थी, इसी लिए हमने मंसूर को प्रधानमंत्री लिखा है।
इस प्रकार मंसूर अंतत: अपने उद्देश्य में सफल हुआ और ऐसा प्रधानमंत्री साबित हुआ कि जिसकी मिसाल अन्दलुस के इतिहास में नहीं मिलती। वह कहने को प्रधानमंत्री था, परन्तु सही अर्थों में हुक्मरान वही था। अपने दोस्तों से जो वादे किए थे उनको उसने पूरा किया।
उत्तर के ईसाई रियासतों से मुसलमानों की बराबर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। ये हुकूमतें जब भी मौक़ा देखती थीं इस्लामी क्षेत्रों पर आक्रमण कर देती थीं। मंसूर ने अपने 28 वर्ष के शासन-काल में उनके विरुद्ध पचास लड़ाइयाँ लड़ीं और उन तमाम रियासतों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया।
मंसूर जब जिहाद से वापस क़ुरतुबा लौटता तो रास्ते में जनता हज़ारों की तादाद में उसे देखने आती और क़ुरतुबा की जनता दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती।
मंसूर ने उत्तर की रियासतों को अधीन बनाने के अलावा अफ़्रीक़ा में भी सल्तनत की सीमाओं में विस्तार किया और मराकश के लगभग तमाम इलाक़े को अपनी सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। मंसूर के समय में अन्दलुस जितना शक्तिशाली हुआ उतना पहले कभी नहीं था। उसने अन्दलुस की हुकूमत को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया।
लड़ाई के मैदान में जो धूल उसके कपड़ों पर जम जाती थी, उसको मंसूर कपड़े से झाड़कर एक डब्बे में रख लेता था। अपने इन्तिक़ाल के समय उसने यह वसीयत की कि यह धूल मेरे शरीर पर छिड़क दी जाए। अतः जब उसका इन्तिक़ाल हुआ तो ऐसा ही किया गया।
मंसूर को इमारतें बनवाने में बड़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में उसका सबसे बड़ा कारनामा 'मस्जिदे क़ुरतुबा का विस्तार' है। उसने क़ुरतबा की मसजिद को दुगुना कर दिया। जब उसने मस्जिद के विस्तार के लिए आस-पास के मकान उसमें शामिल करने चाहे तो और सब लोगों ने ख़ुशी से अपने मकान उसके हाथ बेच दिए, सिर्फ़ एक बूढ़ी औरत अड़ गई और शर्त रखी कि बादशाह जब तक उसे खजूरों के बाग़वाला मकान मुफ़्त भेंट नहीं करेंगे वह अपना मकान नहीं देगी। मंसूर ने उस औरत की इच्छानुसार मकान की तलाश कराई। जब औरत ने मकान पसंद कर लिया तो मंसूर ने वह मकान भी उसे दे दिया और उसके मकान की पूरी क़ीमत भी उसे अदा कर दी।
मंसूर ने जनता के फ़ायदे के बहुत काम किए। पुल बनवाए, नहरें खुदवाईं और सड़कें बनवाईं। उसे न्याय एवं इनसाफ़ का इतना ख़याल था कि वह किसी की सिफ़ारिश नहीं सुनता था। एक बार क़ुरतुबा के क़ाज़ी ने उसके एक दरबारी से हलफ़ लिए बिना ही फ़ैसला कर दिया। उस फ़ैसले की ख़बर उसे हुई तो उसने आदेश दिया कि शरीअ़त का क़ानून सबके लिए एक जैसा है हमारे दरबारी से भी हलफ़ लो। मंसूर के उस दरबारी ने अपने पद के घमंड में हलफ़ उठाने से इनकार कर दिया। मंसूर ने जब यह देखा तो उसे नौकरी से अलग कर दिया।
मंसूर रात को वेश बदलकर शहर का गश्त किया करता था। रात को बहुत कम सोता था और इस प्रकार लोगों के कष्ट मालूम करता और फिर उन्हें दूर करता था।
मंसूर के बाद उसके बेटे अल-मुज़फ़्फ़र (393 हि०/1002 ई० से 399 हि०/1008 ई०) ने छः साल सफलता से हुकूमत की बागडोर सँभाली, परन्तु उसके मरने के बाद जब उसके भाई अब्दुर्रहमान संचोल ने हुकूमत संभाली तो उमवी ख़ानदान के लोगों ने उसके विरुद्ध बग़ावत कर दी। उन लोगों को यह शिकायत थी कि बनू आमिर (मंसूर का असल नाम मुहम्मद बिन अबी आमिर था इसलिए वह और उसकी औलाद बनू आमिर कहलाती है) ने ख़लीफ़ा को बिलकुल बेबस कर दिया है और ख़ुद हुकूमत पर क़ाबिज़ हो गए हैं। अब्दुर्रहमान इस बग़ावत में मारा गया। ख़लीफ़ा हिशाम शाही ख़ानदान के एक दूसरे उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो गया। परन्तु इस बग़ावत ने बनू आमिर की हुकूमत ही ख़त्म नहीं की बल्कि अन्दलुस में इस्लामी हुकूमत की जड़ें हिला दीं। हर ओर अशान्ति फैल गई। बीस साल की अवधि में क़ुरतुबा की गद्दी पर कई उमवी शहज़ादे बैठे और हालात बिगड़ते चले गए, यहाँ तक कि 422 हि०/1030 ई० में उमवी हुकूमत का अन्त हो गया।
सांस्कृतिक उन्नति
अन्दलुस (Andalus) के उमवी ख़ानदान ने 138 हि०/755 ई० से 422 हि०/1030 ई० तक हुकूमत की। अन्दलुस के इतिहास का यह बड़ा शानदार दौर है। मुसलमानों ने इस ज़माने में राजनीतिक हैसियत से अन्दलुस में जो उन्नति की वैसी उन्नति फिर कभी नहीं की। अन्दलुस की राजधानी क़ुरतुबा उस दौर में सारी दुनिया में बग़दाद के बाद दूसरा बड़ा शहर बन गया था। उद्योग-धंधे, खेती और व्यापार में ख़ूब प्रगति हुई। अन्दलुस के उमवी हुक्मरान ज्ञान एवं कला के ऐसे ही प्रेमी थे जैसे कि अब्बासी ख़लीफ़ा। परन्तु अन्दलुस में चूँकि इस्लामी हुकूमत का प्रारंभ देर से हुआ और यह मुल्क इस्लाम के प्रारंभिक केन्द्रों इराक़ और मिस्र से बहुत दूर था, इसलिए यहाँ ज्ञान एवं कला की प्रगति बाद में प्रारंभ हुई। और इसी कारण इस दौर में हमें अन्दलुस में बड़े-बड़े आलिमों के नाम बहुलता से नज़र नहीं आते जैसे अब्बासी ख़िलाफ़त में नज़र आते हैं।
चौथी हिजरी शताब्दी में जबकि अन्दलुस में अब्दुर्रहमान आज़म, अल-हकम और मंसूर का शासन था, अन्दलुस के इतिहास का स्वर्णिम काल है। उस काल में इल्म की प्रगति बहुत तेज़ी से हुई और कई प्रमुख विद्वान पैदा हुए। उनमें एक ज़ुहरावी हैं। ज़ुहरावी अब्दुर्रहमान और अल-हकम के दरबारी चिकित्सक थे। ज़ुहरावी सर्जरी यानी चीर-फाड़ के माहिर थे। अब तक मुसलमान चिकित्सकों ने दवा के द्वारा इलाज करने में तो दक्षता प्राप्त की थी, परन्तु सर्जरी की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ज़ुहरावी पहले मुसलमान चिकित्सक हैं जिन्होंने सर्जरी-विद्या में दक्षता प्राप्त की। जिस प्रकार राज़ी इतिहास में सबसे बड़े चिकित्सक हुए हैं, उसी प्रकार ज़ुहरावी सबसे बड़े मुसलमान सर्जन थे। ज़ुहरावी ने 'अत-तसरीफ़' के नाम से सर्जरी पर एक किताब लिखी जो आज भी मौजूद है। यूरोप में सर्जरी का प्रारंभ इसी किताब के द्वारा हुआ।
उस काल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार 'अबू अली क़ाली' हैं। उनकी किताब 'अमाली' अरबी भाषा में इतिहास एवं साहित्य की बेहतरीन किताबों में गिनी जाती है।
'इब्ने अब्दे रब्बिही' भी उस काल के एक प्रसिद्ध कवि साहित्यकार हैं। कुछ लोग उन्हें अन्दलुस का सबसे बड़ा कवि समझते हैं। परन्तु उनकी प्रसिद्धि एक काव्य ग्रन्थ 'अक़्दुल फ़रीद' के कारण है। यह किताब चार खण्डों में है और अमाली की भाँति इतिहास और साहित्य की बेहतरीन पुस्तकों में से है।
उमवी काल के दीनी आलिमों में यह्या बिन यह्या (152 हि०/769 ई० से 234 हि०/848 ई०) बहुत प्रतिष्ठित हैं। उनका सम्बन्ध उमवी हुकूमत के प्रारम्भिक काल से है। यह्या मदीने के प्रसिद्ध मुहद्दिस (हदीस के विद्वान) इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) के शागिर्द हैं और कई साल तक उनके साथ रहे हैं। वे एक बार दूसरे शागिर्दों के साथ इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) से पढ़ रहे थे कि बाहर से एक हाथी गुज़रा। हाथी देखने के लिए सभी शागिर्द उठकर चले गए, परन्तु यह्या नहीं गए। इमाम साहब ने उनसे कहा, "हाथी तुम्हारे देश में नहीं होता है, जाओ देख आओ।" यह्या ने जवाब दिया, "मैं अन्दलुस से यहाँ तक इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, हाथी देखने नहीं आया।" इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) इस जवाब से बहुत ख़ुश हुए। वे उन्हें आक़िले अन्दलुस (अन्दलुस का बुद्धिमान) कहते थे।
क़ाज़ी यह्या अन्दलुस के दूसरे अमीर (ख़लीफ़ा) हिशाम के पोते अब्दुर्रहमान द्वितीय के काल में थे और उनका हुकूमत में इतना प्रभाव था कि अब्दुर्रहमान उनके मशविरे से तमाम क़ाज़ी नियुक्त करता था और वह जिसे चाहते थे इस पद से हटा देते थे। उनके फ़ैसले में बादशाह किसी प्रकार की रुकावट नहीं करता था। वे इतने साहसी थे कि बादशाह के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर देते थे। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) की किताब 'मुवत्ता' को अन्दलुस में क़ाज़ी यह्या ही लाए।
क़ुरतुबा (Cordova)
उमवी काल में क़ुरतुबा ख़लीफ़ा का मुख्यालय था और देश का सबसे बड़ा शहर था। अपनी विशालता, शानदार इमारतों और सुन्दरता के कारण इसको उरूसुल-बिलाद यानी शहरों की दुल्हन कहा जाता था। यह शहर ज्ञान एवं कला और उद्योग-धंधों का बहुत बड़ा केन्द्र था। यहाँ की इमारतों में जामे क़ुरतुबा (क़ुरतुबा की जामा मस्जिद) और मदीनतुज़-ज़ुहरा के भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने थे। क़ुरतुबा के हालात चूँकि हमने 'यूरोप के उस्ताद' वाले अध्याय में विस्तार से बयान किए हैं, इसलिए यहाँ अन्दलुस के कुछ दूसरे बड़े शहरों का हाल लिखा जाता है, ताकि यह मालूम हो सके कि अन्दलुस जैसे छोटे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में बड़े-बड़े और विकसित शहर मौजूद थे।
इशबीलिया (Sevilla )
यह अन्दलुस का दूसरा बड़ा शहर था। उद्योग-धंधे और जहाज़-निर्माण का केन्द्र था। अल-कबीर नदी के किनारे बसे होने के कारण बड़े-बड़े जहाज़ शहर तक आ जाते थे। युद्ध सम्बंधी यंत्रों के उद्योग में यहाँ की कमान बहुत अच्छी समझी जाती थी। जनता सुरुचि रखनेवाली और सफ़ाईपसंद थी। वास्तुकला और बाग़बानी में माहिर समझी जाती थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन अति सुन्दर बनाते थे। इन्हें संगीत से विशेष दिलचस्पी थी। अतः मशहूर था कि जब कोई आलिम (विद्वान) इशबीलिया में मर जाता था तो उसकी किताबें क़ुरतुबा में बेची जाती थी और जब क़ुरतुबा में कोई संगीतकार मरता था तो उसके वाद्य-यंत्र अशबीलिया लाकर बेचे जाते थे। यह शहर साढ़े पाँच सौ साल तक मुसलमानों के क़बज़े में रहा।
तुलैतिला (Toledo)
यह उस जगह के निकट स्थित था जहाँ अब स्पेन की राजधानी मेड्रिड है। यहाँ की बनी हुई तलवार अन्दलुस में सबसे अच्छी समझी जाती थी। यहाँ ज़ाफ़रान की बड़े पैमाने पर खेती होती थी और उच्च कोटि की समझी जाती थी। यहाँ की जलवायु अनाज के लिए इतनी मुनासिब थी कि अनाज सत्तर साल तक ख़राब नहीं होता था। यह शहर 386 साल मुसलमानों के क़बज़े में रहा।
बलंसिया (Velencia)
उद्यानों की बहुलता और ज़ाफ़रान की बड़े पैमाने पर खेती के कारण इसे ख़ुशबुओं का शहर कहा जाता था। यहाँ की रोग़नी ईंटें और रेशमी कपड़े दूर-दूर तक मशहूर थे। शातिबा (Jativa) का शहर जो यूरोप में काग़ज़ उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र था, बलंसिया के निकट ही था। यहाँ की जनता दीनदारी (धर्मपरायणता), नैतिकता और आतिथ्य सत्कार में प्रसिद्ध थी। यह सिंचाई व्यवस्था का बड़ा केन्द्र था। यह शहर 532 साल मुसलमानों के क़बज़े में रहा।
मुरसिया (Murcia)
यह भी बलंसिया की तरह कृतिम सिंचाई व्यवस्था का केन्द्र था। सुन्दर एवं दर्शनीय शहरों में गिना जाता था। क़ालीन और धारीदार कपड़ों के उद्योग का केन्द्र था। इन कपड़ों से दीवारों को सजाया जाता था। यह शहर 575 साल मुसलमानों के पास रहा।
अल-मरिया
यह मुल्क में रेशम उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र था और तरह-तरह के कपड़े यहाँ तैयार किए जाते थे। यहाँ रेशम बनाने के आठ सौ कारख़ाने थे। यह हथियार साज़ी और जहाज़ के निर्माण का भी केन्द्र था। मेवे और फलों की यहाँ बहुलता थी। बहुत बड़ा बन्दरगाह होने के कारण यह व्यापार का केन्द्र था और सारे यूरोप और अफ़्रीक़ा के जहाज़ यहाँ आते थे। यहाँ की जनता का पेशा व्यापार था, जिसके कारण ये सम्पूर्ण अन्दलुस में सबसे अधिक धनी थे। यह शहर 790 साल मुसलमानों के पास रहा।
मालक़ा (Malaga)
यह शहर भी अल-मरिया की तरह एक बड़ी बन्दरगाह था। यहाँ के इंजीर दूर-दूर तक मशहूर थे और भारत तक जाते थे। पता चलता है कि आख़िरी दौर में यहाँ की जनता नैतिक पतन का शिकार हो गई थी और शराब बनाने लगी थी। यहाँ की शराब अच्छी समझी जाती थी। अतः एक लतीफ़ा प्रसिद्ध है कि जब यहाँ का एक हुक्मरान मरने लगा तो लोगों ने उससे कहा, “ख़ुदा से माफ़ी की दुआ करो।" तो हुक्मरान ने हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत की तमाम चीज़ें माँगता हूँ, जैसे इशबीलिया के अंगूर और मालक़ा की शराब।
इस शहर पर मुसलमानों का 800 साल क़बज़ा रहा।
अन्दलुस की उमवी हुकूमत
(138 हि०/756 ई० से 422 हि०/1030 ई०)
1. अब्दुर्रहमान अद-दाख़िल - 138 हि०/756 ई० से 172 हि०/788 ई०
2. हिशाम प्रथम - 172 हि०/788 ई० से 180 हि०/796 ई०
3. हकम प्रथम - 180 हि०/796 ई० से 206 हि०/822 ई०
4. अब्दुर्रहमान अल-अवसत - 206 हि०/822 ई० से 238 हि०/852 ई०
5. मुहम्मद प्रथम - 238 हि०/852 ई० से 273 हि०/886 ई०
6. मुन्ज़िर - 273 हि०/886 ई० से 275 हि०/888 ई०
7. अब्दुल्लाह - 275 हि०/888 ई० से 300 हि०/912 ई०
8. अब्दुर्रहमान अन-नासिर - 300 हि०/912 ई० से 350 हि०/961 ई०
9. हकम द्वितीय - 350 हि०/961 ई० से 366 हि०/976 ई०
10. हिशाम द्वितीय - 366 हि०/976 ई० से 399 हि०/1009 ई०
मंसूर (366 हि०-393 हि०) हिशाम द्वितीय का प्रधानमंत्री था। हिशाम द्वितीय के बाद अन्दलुस की उमवी हुकूमत का पतन हो गया और बाईस साल की अवधि में दस हुक्मरान गद्दी पर बैठे और उतारे गए। 422 हि०/1030 ई० में उमवी हुकूमत समाप्त हो गई।
अध्याय-19
बर्बर इस्लाम की ढाल बन गए
उमवी हुकूमत के पतन के बाद अन्दलुस के मुसलमानों में गृहयुद्ध छिड़ गया और मुल्क में कई आज़ाद हुकूमतें क़ायम हो गईं। उन हुकूमतों में निम्न तीन हुकूमतें उल्लेखनीय हैं—
1. बनू ज़ुन्नून
यह बर्बर ख़ानदान की हुकूमत थी और इसका केन्द्र-स्थल शहर तुलैतिला (Toledo) था। यह हुकूमत 428 हि०/1036 ई० से 478 हि०/1085 ई० तक क़ायम रही। इसके बाद यह शहर ईसाइयों के क़बज़े में चला गया। परन्तु मुसलमान इस शहर में 898 हि०/1492 ई० में ग़रनाता (Garnada) की पराजय तक मौजूद रहे। इसके बाद उन्हें शहर से निकाल दिया गया। यहाँ के ईसाई भी मुसलमानों की तरह अरबी बोलते थे। मुसलमानों के बाद 1250 ई० से 1400 ई० तक यह शहर मुसलमानों के ज्ञान का, पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद करने का, बहुत बड़ा केन्द्र रहा। यहाँ का हुक्मरान अलफ़ांसो दशम् (1252 ई० से 1284 ई०) ख़ुद को दो मिल्लतों (समुदायों) यानी ईसाई और मुसलमानों का बादशाह कहता था। उसके ज़माने में अरबी किताबों के सबसे ज़्यादा अनुवाद हुए।
2. सरक़स्ता (Zaragoza)
इस शहर पर दो भिन्न ख़ानदानों ने 403 हि०/1012 ई० से 503 हि०/1109 ई० तक हुकूमत की। 503 हि०/1109 ई० से 512 हि०/1118 ई० तक यह शहर मराबतीन के क़बज़े में रहा। इसके बाद ईसाइयों का आधिपत्य हो गया। तुलैतिला के बाद यह इस्लामी अन्दलुस का दूसरा बड़ा शहर था जो ईसाइयों के क़बज़े में गया।
3. बनी अक़तस
यह हुकूमत 433 हि०/1042 ई० से 486 हि०/1093 ई० तक क़ायम रही। फिर मराबतीन और उसके बाद मुवह्हिदीन इस शहर पर क़ाबिज़ हो गए। इस हुकूमत का प्रधान स्थल बतल्यूस (Badajoz) था।
इन हुकूमतों के कारण इन शहरों की बड़ी तरक़्क़ी हुई। ये बादशाह ज्ञान एवं साहित्य के बड़े संरक्षक थे और इनमें कुछ बादशाह लेखक और कवि भी हुए हैं। जैसे तुलैतिला के बादशाह अल-मामून (435 हि ०/1043 ई० से 499 हि०/1105 ई०) को गणित में बहुत रुचि थी और उसने अपनी राजधानी में अजीबो ग़रीब पनघड़ियाँ बनाई थीं। ये पनघड़ियाँ तुलैतिला के प्रसिद्ध खगोलविद् अबुल क़ासिम अब्दुर्रहमान ने बनाई थीं। इन पनघड़ियों से वक़्त के अतिरिक्त दिन और तारीख़ भी मालूम की जा सकती थी।
शहर के बाहर 'ताजा' नामक नदी के किनारे दो हौज़ बनाए गए थे जो चाँद के बढ़ने के साथ-साथ भरते जाते और चाँद के घटने के साथ-साथ ख़ाली होते जाते थे। चौदहवीं रात को जब चाँद पूरा हो जाता था तो ये हौज़ पूरी तरह भर जाते थे। उसके बाद ख़ाली होना शुरू होते जाते थे और उन्नीसवें दिन, रात को तो बिलकुल ख़ाली हो जाते थे।
एक अजीब बात इन हौज़ों में यह थी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से इनमें पानी डाले या उनमें से पानी निकाल ले तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। जितना पानी बाहर से कोई डालता था, हौज़ में गिरते ही लुप्त हो जाता था और जितना पानी कोई निकालता, तुरंत उतनी कमी पूरी हो जाती थी।
जब तुलैतिला में ईसाइयों का क़बज़ा हो गया तो पचास वर्ष बाद ईसाई बादशाह ने इन हौज़ों का रहस्य मालूम करना चाहा और एक हौज़ को खुदवाना शुरू किया जिससे नुक़सान पहुँच गया और हौज़ों में पानी आना बन्द हो गया। इन हौज़ों के खंडहर अब भी तुलैतिला शहर में मौजूद हैं।
हाँ, तो हम यह कह रहे थे कि बनी उमैया के बाद अन्दलुस में कई छोटी-छोटी हुकूमतें क़ायम हो गई थीं जो आपस में लड़ती रहती थीं। इसलिए उत्तर के ईसाइयों का, जिनमें क़शताला की हुकूमत बहुत शक्तिशाली थी, मुक़ाबला नहीं कर सकती थीं। ईसाई धीरे-धीरे मुसलमानों के शहरों पर क़बज़ा करते चले गए। उन्होंने 478 हि०/1085 ई० में तुलैतिला भी जीत लिया और इशबीलिया के बादशाह मुअतमिद को ख़िराज (टैक्स) देने पर मजबूर कर दिया। मुअतमिद की हुकूमत अन्दलुस की हुकूमतों में सबसे बड़ी हुकूमत थी। इशबीलिया के अतिरिक्त क़ुरतुबा भी उसके क़बज़े में था। मुसलमानों ने जब देखा कि मुअतमिद भी, जो सबसे बड़ा बादशाह था, ईसाइयों के मुक़ाबले में नाकाम रहा तो उन्होंने अन्दलुस को ईसाइयों से बचाने के लिए समुद्र पार अमीर यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन से, जिसने उस काल में मराकश में एक शक्तिशाली हुकूमत क़ायम कर ली थी, मदद माँगी।
यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन
(453 हि०/1061 ई० से 500 हि०/1107 ई०)
यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन (453 हि० से 500 हि०) मराकश के दक्षिण में रेगिस्तानी इलाक़े का रहनेवाला था। उसने और उसके साथियों ने अफ़्रीक़ा के विशाल रेगिस्तान और उसके दक्षिण में रहने वाले अर्द्ध-वहशी बर्बर और हबशी लोगों से कई साल तक लड़ाइयाँ कीं और उनके इलाक़े में अपनी हुकूमत सीनीगाल नदी तक बढ़ा दी थी। ये लोग बर्बरों के ख़िलाफ़ जिहाद ही नहीं करते थे, बल्कि उनमें इस्लाम का प्रचार-प्रसार भी करते थे और इस प्रकार उनकी तबलीग़ से अनगिनत बर्बरों और हबशियों ने इस्लाम क़बूल किया। इस्लाम के प्रचार-प्रसार का यह काम यूसुफ़ के चाचा अब्दुल्लाह बिन यासीन की निगरानी में होता था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए सीनीगाल नदी के एक टापू में एक ख़ानक़ाह बना ली थी। प्रारम्भ में यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन इस काम में अपने चाचा के साथ था। परन्तु बाद में यूसुफ़ उत्तर की ओर आ गया और यहाँ फ़ास और दूसरे शहर फ़तह करके अटलस पहाड़ की वादी में शहर मराकश की बुनियाद डाली। अन्दलुस के मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल यूसुफ़ से मदद माँगने के लिए इसी शहर मराकश में आया। यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन मदद के लिए तैयार हो गया और एक शक्तिशाली फ़ौज के साथ अन्दलुस रवाना हुआ। ईसाई बादशाह अलफ़ान्सो ने 'ज़ुल्लाक़ा' के मैदान में मुसलमानों का मुक़ाबला किया। इस घमासान युद्ध के बाद यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन ने अलफ़ांसो को 479 हि०/1086 ई० में करारी शिकस्त दी।
इस युद्ध ने एक क्रान्ति ला दी। ईसाइयों के साहस जवाब दे गए और यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन ने अन्दलुस की छोटी-छोटी मुसलमान हुकूमतों को समाप्त कर उन्हें अपनी सल्तनत में मिला लिया।
यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन बहुत ही नेक और न्यायप्रिय हुक्मरान था। उसकी ज़िन्दगी बड़ी साधारण थी। इस्लामी इतिहास में उसका बड़ा महत्त्व है। अफ़्रीक़ा के विशाल रेगिस्तान में इस्लाम के प्रचार और अन्दलुस में ईसाइयों के ज़ोर को रोकना उसका बहुत बड़ा कारनामा है। शहर मराकश का निर्माण भी उसके महान कारनामों में गिना जाता है, क्योंकि इस प्रकार उसने एक अर्द्ध-पशुवत् इलाक़े में राजधानी बना कर सभ्यता एवं ज्ञान की बुनियाद डाल दी।
यूसुफ़ ने कुल पचास साल हुकूमत की। उसकी क़ायम की हुई सल्तनत 'दौलत मराबतीन' (453 हि०/1061 ई० से 541 हि०/1147 ई०) कहलाती है। यूसुफ़ के इन्तिक़ाल के बाद यह हुकूमत चालीस साल और क़ायम रही। उसके बाद जिन लोगों की हुकूमत हुई वह 'मुवह्हिदीन' कहलाते हैं।
मुवह्हिदीन की ख़िलाफ़त (524 हि०/1130 ई०-667 हि०/1269 ई०)
मुवह्हिदीन एक जमाअत का नाम था। मुल्क का सुधार करना और मुसलमानों के अन्दर जो ख़राबियाँ पैदा हो गई थीं उन्हें दूर करना, इनका उद्देयश्य था। इस जमाअत को मुहम्मद बिन तूमर्त ने क़ायम किया था। मुहम्मद बिन तूमर्त बहुत बड़े आलिम थे। वह सलजूक़ी काल के प्रसिद्ध आलिम इमाम ग़ज़ाली के शागिर्द थे और उन्हीं की प्रेरणा से इब्ने तूमर्त ने पश्चिम में, जो अब मराकश कहलाता है, अपना सुधार आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन का उद्देश्य सामाजिक एवं नैतिक सुधार था। वह जहाँ कहीं शरीअ़त के विरुद्ध कोई हरकत देखते उस पर टोकते, शराब के बर्तन तोड़ देते, गाने-बजाने के यंत्र उठाकर फेंक देते। इब्ने तूमर्त ने केवल सख़्ती ही नहीं की, उन्होंने नसीहतें और उपदेशों के द्वारा लोगों में इस्लामी रूह पैदा करनी शुरू कर दी। उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि देखकर मराबतीन की हुकूमत को ख़तरा पैदा हुआ और उन्हें मराकश से निकाल दिया गया। वे दूसरे शहर अग़मात में आ गए, लेकिन यहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। अब वह अपने वतन हरग़ा (अरग़न) चले गए जो पहाड़ों में था। यहाँ के लोगों ने हज़ारों की तादाद में उनकी दावत क़बूल की। उन्होंने फ़ौजी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और मज़हबी शिक्षा भी। अब मराबतीन की फ़ौज यहाँ भी आ गई और बस्ती का घेराव कर लिया। परन्तु अब इब्ने तूमर्त के साथी जिनका नाम मुवह्हिदीन था, मुक़ाबला करने के योग्य हो गए थे। इसलिए बड़ी सख़्त लड़ाई हुई और सरकारी फ़ौज को पराजय का मुँह देखना पड़ा। इसके बाद मुवह्हिदीन और मराबतीन के बीच लड़ाइयों का सिलसिला कई साल तक जारी रहा। इब्ने तूमर्त का 524 हि०/1130 ई० में इन्तिक़ाल हो गया। और उनके एक साथी अब्दुल मोमिन को मुवह्हिदीन की जमाअत का अमीर (अध्यक्ष) चुना गया।
अब्दुल मोमिन (524 हि०/1130 ई० से 558 हि०/1163 ई०)
अब्दुल मोमिन के काल में मुवह्हिदीन ने बड़ी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने 541 हि०/1147 ई० में मराकश पर क़बज़ा करके मराबतीन की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद अब्दुल मोमिन ने एक फ़ौज अन्दलुस भेजी जिसने मराबतीन की हुकूमत को वहाँ से भी ख़त्म कर दिया। अब्दुल मोमिन ने अब पूरब का रुख़ किया और तराबुलस (Tripoli) तक अपनी सल्तनत का विस्तार किया। उस ज़मानें में तराबुलस, तूनिस और महदिया पर जो उस ज़माने में अफ़्रीक़ा कहलाता था, नारमन क़ौम क़ाबिज़ थी। ये लोग ईसाई थे और उनकी हुकूमत सक़लिया टापू में क़ायम थी। जिस ज़माने में यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी लड़ाइयाँ शुरू की थीं और शाम के समुद्र तटीय इलाक़े और बैतुल मक़दिस पर क़बज़ा किया था, लगभग उसी ज़माने में नारमनों ने क़ैरवान, तूनिस और तराबुलस के इलाक़ों पर हमले शुरू कर दिए। उस ज़माने में यहाँ संहाजी (363 हि०/973 ई० से 543 हि०/1148 ई०) ख़ानदान की हुकूमत थी जिसे 'बनू ज़ैरी' भी कहा जाता है। यह हुकूमत फ़ातिमी ख़िलाफ़त के पतन के बाद क़ायम हुई थी। जब इस हुकूमत का पतन हुआ तो नारमानों ने इन शहरों पर क़बज़ा कर लिया। इस प्रकार ईसाई यूरोप ने एक ही समय में इस्लामी दुनिया के दो इलाक़ों यानी शाम के समुद्र तटीय क्षेत्र और अफ़्रीक़ा में अपनी हुकूमत क़ायम कर ली। परन्तु जिस प्रकार पूरब में नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन ने ईसाई हुकूमत को ख़त्म किया उसी तरह अब्दुल मोमिन ने तूनिस और तराबुलस फ़तह करके पश्चिम में ईसाई वर्चस्व का अन्त कर दिया। मराबतीन और मुवह्हिदीन की लड़ाइयों के ज़माने में अन्दलुस में ईसाई फिर ज़ोर पकड़ गए थे। अब्दुल मोमिन ने अन्दलुस में भी उनके हमले को रोका।
अब्दुल मोमिन सुल्तान नूरुद्दीन का समकालीन था और उसका मुसलमानों पर उतना ही उपकार है जितना नूरुद्दीन और उसके उत्तराधिकारी सलाहुद्दीन का है। अब्दुल मोमिन ने जितनी विशाल हुकूमत क़ायम की उतनी बड़ी हुकूमत उत्तरी अफ़्रीक़ा के किसी मुसलमान ने अब तक क़ायम नहीं की थी और न ही उसके बाद फिर उतनी बड़ी हुकूमत क़ायम हुई।
अब्दुल मोमिन इस्लामी इतिहास का बहुत बड़ा हुक्मरान है। वह एक मामूली इनसान था। उसने अपनी योग्यता से एक विशाल सल्तनत की बुनियाद डाली। वह शरीअ़त का बड़ा पाबन्द था और उसने इसकी कोशिश भी की कि क़ुरआन एवं सुन्नत के अनुसार हुकूमत की जाए। वह ज्ञान एवं कला का भी बड़ा संरक्षक था। उसके दौर के सुप्रसिद्ध दार्शनिक इब्ने तुफ़ैल (मृत्यु-1185 ई०) और उस काल के सबसे बड़े चिकित्सक अब्दुल मलिक बिन ज़ुहर उसके दरबार से संबद्ध थे।
अन्त में अब्दुल मोमिन ने एक बड़े जिहाद का एलान किया। अब तक यूरोपवाले इस्लामी हुकूमतों पर आक्रमण करते थे। अब अब्दुल मोमिन ने ख़ुद यूरोप पर हमला करने का इरादा किया। जिहाद की ज़ोर-शोर से तैयारियाँ शुरू कर दीं। चार सौ जंगी जहाज़ बनाए गए और तीन लाख दस हज़ार सवार और एक लाख पैदल सैनिक एकत्रित किए। परन्तु अभी यह फ़ौज रवाना नहीं हुई थी कि अब्दुल मोमिन का इन्तिक़ाल हो गया। यदि अब्दुल मोमिन का इन्तिक़ाल न होता तो शायद आज यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के क़बज़े में होता। अब्दुल मोमिन का 558 हि०/1163 ई० में 58 साल की उम्र में इन्तिक़ाल हुआ।
अब्दुल मोमिन के बाद मुवह्हिदीन की जमाअत ने उसके लड़के यूसुफ़ (558) हि०/1163 ई० से 580 हि०/1184 ई०) को अमीर नियुक्त किया। यूसुफ़ ने 22 साल तक बड़ी दक्षता से हुकूमत की। अन्दलुस के शहर इशबीलिया का बहुत विकास हुआ। यूसुफ़ उमवी ख़लीफ़ा अल-हकम की तरह ज्ञान एवं साहित्य का शौक़ीन था। उसने मराकश में जो पुस्तकालय स्थापित किया था, उसमें भी अल-हकम के पुस्तकालय की तरह चार लाख किताबें थीं। उस ज़माने में सबसे बड़े दार्शनिक इब्ने तुफ़ैल और इब्ने रुश्द (Averros) का उसके दरबार से संबंध था।
याक़ूब अल मंसूर
(580 हि०/1184 ई० से 595 हि०/1199 ई०)
मुवह्हिदीन में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुक्मरान यूसुफ़ का लड़का याक़ूब अल-मंसूर हुआ है। याक़ूब की सबसे अधिक प्रसिद्धि उस फ़तह के कारण है जो उसने उत्तरी अन्दलुस के ईसाई हुक्मरान अलफ़ांसो पर 'अरक' के मैदान में प्राप्त की। अलफ़ांसो और अमीर याक़ूब के बीच पाँच साल के लिए संधि हो गई थी, परन्तु अलफ़ांसो ने संधि तोड़कर इस्लामी इलाक़े पर हमला कर दिया। याक़ूब को जब सूचना मिली तो मराकश से अन्दलुस पहुँचा और अरक नामक स्थान पर अलफ़ांसो को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त दी जैसी कि सौ साल पहले यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन 'ज़ल्लाक़ा' में दे चुका था। उसके बाद याक़ूब ने अलफ़ांसो की राजधानी तुलैतिला का घेराव कर लिया। यह शहर फ़तह होने ही वाला था कि अलफ़ांसो ने अपनी बूढ़ी माँ को अमीर याक़ूब के पास भेजकर क्षमा माँगी। याक़ूब अपने दुश्मन की बूढ़ी माँ की दरख़्वास्त को रद्द न कर सका और दस साल के लिए संधि करके वापस हो गया। इस प्रकार याक़ूब अल-मंसूर की दयालुता के कारण तुलैतिला का ऐतिहासिक शहर दोबारा मुसलमानों के हाथों में आने से रह गया।
याक़ूब की ज़िन्दगी आम बादशाहों की तरह नहीं थी। वह सादा ज़िन्दगी गुज़ारता था। मामूली कपड़े पहनता था। पाँचों वक़्त की नमाज़ मस्जिद में आकर आम मुसलमानों के साथ पढ़ता था। न्याय का इतना ख़याल रखता था कि राह चलते फ़रयादी के लिए सवारी रोक लेता। एक बार दो व्यक्ति आधे दिरहम पर झगड़ा करते हुए उसके पास आए। मंसूर ने उनसे कहा कि जब शहर में क़ाज़ी मौजूद है तो ये छोटे-छोटे झगड़े मेरे सामने क्यों लेकर आते हो? इसके बाद उसने दोनों को तंबीह के तौर पर हल्की सी सज़ा दी। इस घटना से स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति कितनी आसानी से उसके पास पहुँच सकता था।
उसके काल में आलिमों, फ़क़ीहों (इस्लामी विधि-विधान के ज्ञाता) और मुहद्दिसों (हदीस के ज्ञाता) के वज़ीफ़े तय थे। उसने सड़कें और जगह-जगह सरायें बनवाईं।
प्रत्येक साल लावारिस यतीम बच्चों का ख़त्ना कराना, फिर उनमें पैसे, रोटी, कपड़े और फल बाँटना, इसी प्रकार बूढ़ी औरतों और ख़ानक़ाही लोगों को वज़ीफ़े देना उसका नियम था।
अमीर याक़ूब ने अपनी सल्तनत में मदरसे और अस्पताल भी खुलवाए। उनमें मराकश का अस्पताल बड़ा शानदार था। यह अस्पताल एक बहुत बड़े मैदान में बनाया गया था। इमारतें बहुत मज़बूत थीं और उनमें सुन्दर चित्रकारी थी। कमरों के फ़र्श सीप के बनाए गए थे और उनके ऊपर क़ालीन बिछे रहते थे। अस्पताल के मैदान में तरह-तरह के पेड़ थे, जिनमें फूलों और फलों के पेड़ भी थे। अस्पताल के अहाते में ऐसी नहरें जारी थीं कि उनका पानी नालियों के रूप में हर मकान में पहुँचता था। मैदान के बीच में चार हौज़ थे जिनमें एक सफ़ेद संगमरमर का था।
इस अस्पताल में मरीज़ों को जो खाना दिया जाता था केवल उसका ख़र्च तीस दीनार (एक सौ पचास रुपये) रोज़ाना था। दवाओं पर जो ख़र्च होता था वह उसके अलावा था। विभिन्न प्रकार के शर्बत, रोग़न और सुर्मे आदि बनाने के लिए अत्तार नियुक्त थे। मरीज़ों के लिए गर्मियों और सर्दियों के ज़माने में दिन और रात में इस्तेमाल के लिए अलग-अलग लिबास होते थे जो अस्पताल की ओर से दिए जाते थे। जब मरीज़ स्वस्थ हो जाता तो यदि वह ग़रीब होता तो उसे जाते वक़्त इतना धन दिया जाता कि वह तमाम उम्र चैन से गुज़ार सके। जब कोई परदेसी मराकश आने के बाद किसी मर्ज़ में घिर जाता उसे भी अस्पताल में पहुँचा दिया जाता था।
याक़ूब अल-मंसूर प्रत्येक जुमा को नमाज़ के बाद अस्पताल का स्वयं निरीक्षण करता था। मरीज़ों से मिलकर उनका हाल मालूम करता था और पूछता था कि उनकी देखभाल कैसी हो रही है। याक़ूब का यह नियम उसकी मृत्यु तक जारी रहा।
याक़ूब को इमारतें बनाने का भी बहुत शौक़ था। उसके काल में जैसी इमारतें बनाई गईं उसकी मिसाल उत्तरी अफ़्रीक़ा के इतिहास में इससे पहले नहीं मिलती। उनमें सबसे शानदार इमारत मराकश की 'जामे कुतबिया' की है। इस मस्जिद का मीनार साढ़े तीन सौ फिट ऊँचा है। इस मस्जिद के कुछ साल बाद दिल्ली में क़ुतुब मीनार का निर्माण हुआ, परन्तु कुतबिया का यह मीनार क़ुतुब मीनार से भी सौ फीट ऊँचा है। यह मस्जिद और इसका मीनार आज भी मौजूद हैं। यह मस्जिद कुतबिया इसलिए कहलाती है कि इसके नीचे किताबें बेचनेवालों की दुकानें थीं। उस ज़माने में लिखने-पढ़ने का शौक़ कितना अधिक था इसका अनुमान इससे हो सकता है कि किताबों की इन दुकानों की तादाद दो सौ से ज़्यादा थी।
याक़ूब ने इशबीलिया की जामा मस्जिद में भी मीनार बनवाया। यह मीनार अब 'जीराल्डा' कहलाता है। इसकी ऊँचाई भी तीन सौ फीट है और यह दुनिया के सुन्दरतम मीनारों में गिना जाता है।
जामे कुतबिया की एक दिलचस्प चीज़ मस्जिद का मक़सूरह (मस्जिद में इमाम के खड़े होने की जगह) था। कारीगरों ने यह मक़सूरह इस प्रकार बनाया था कि मंसूर के मस्जिद में प्रवेश करते ही प्रकट हो जाता और जब वह वापस चला जाता तो मक़सूरह लुप्त हो जाता था और मस्जिद की दीवार पहले की तरह बराबर हो जाती थी। याक़ूब अल-मंसूर भी अब्दुल मोमिन और यूसुफ़ की तरह आलिमों, फ़ाज़िलों (विद्वानों) का बड़ा क़द्रदाँ था। अतः इब्ने तुफ़ैल और इब्ने रुश्द का उसके दरबार से भी सम्बन्ध था। इनके अतिरिक्त उस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार और शायर अबू बक्र बिन ज़ुहर भी उसके दरबार से सम्बन्ध रखते थे।
अमीर याक़ूब सुल्तान सलाहुद्दीन का समकालीन था, और उस ज़माने में सारी दुनिया में सिवाए सुल्तान सलाहुद्दीन के और कोई हुक्मरान इन गुणों में उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता था। यह योग्य हुक्मरान 595 हि०/1199 ई० में पंद्रह साल हुकूमत करने के बाद अपने ख़ुदा से जा मिला। उस समय उसकी उम्र केवल चालीस वर्ष थी।
याक़ूब अल-मंसूर के बाद उसका लड़का अन-नासिर गद्दी पर बैठा। उसका काल भी ख़ुशहाली का काल था, परन्तु उसे 609 हि०/1212 ई० में अन्दलुस में 'अल-उक़ाब' नामक स्थान पर ईसाइयों के मुक़ाबले में ऐसी पराजय हुई कि मुवह्हिदीन का ज़ोर टूट गया। अगले साल अन-नासिर का इन्तिक़ाल हो गया और उसके बाद मुवह्हिदीन का पतन प्रारम्भ हो गया। 634 हि०/1237 ई० में बलंसिया पर और 646 हि०/1248 ई० में इशबीलिया पर ईसाइयों का क़बज़ा हो गया। अन्दलुस का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के क़बज़े से निकल गया। ख़ुद मराकश में 667 हि०/1268 ई० में ख़ानदान बनी मरीन ने मुवह्हिदीन की हुकूमत का अन्त कर दिया।
प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने ख़लदून ने मुवह्हिदीन की शासन प्रणाली का उल्लेख इस प्रकार किया है—
“उनकी हुकूमत का यह नियम था कि आलिमों की इज़्ज़त की जाती थी और तमाम मामलात में उनकी सलाह लेकर काम किया जाता था। फ़रियादियों की फ़रियाद सुनी जाती थी, प्रजा पर हाकिम (गवर्नर) अत्याचार करते थे तो उन्हें दण्डित किया जाता था। ज़ालिमों का हाथ रोक दिया जाता था। शाही महलों में मस्जिदें बनवाई गई थीं, तमाम सरहदी रास्ते जहाँ यूरोप की सरहद मिलती थी, फ़ौजी ताक़त से मज़बूत कर दिए गए थे और लड़ाइयों एवं लड़ाइयों में विजयों का सिलसिला जारी था।"
मराबतीन और मुवह्हिदीन की हुकूमतें नस्ल से अरब नहीं थीं बल्कि बर्बर थीं। इसलिए हम इस काल को बर्बर-काल कह सकते हैं। बर्बर जनता इस्लाम से पूर्व अपनी वहशत एवं क्रूरता में प्रसिद्ध थी और उनकी इसी विशेषता के कारण बर्बर शब्द, वहशत एवं ज़ुल्म का पर्यायवाची बन गया था, परन्तु इस्लाम के बाद इन बर्बरों ने जो रचनात्मक काम किए वह अपनी मिसाल आप हैं।
बनी उमैया के पतन के बाद से मुवह्हिदीन के पतन तक दो सौ साल की अवधि होती है। यह समय इस्लामी इतिहास में बहुत महत्त्व रखता है। इसके महत्त्व का कारण एक तो यह है कि अन्दलुस में मुसलमानों में उत्थान का अन्तिम दौर था। उसके बाद पतन शुरू हो गया। इसके महत्व का दूसरा कारण यह है कि इस ज़माने में अन्दलुस में बड़ी ज़बरदस्त बौद्धिक उन्नति हुई और ऐसे-ऐसे लेखक और विद्वान पैदा हुए कि जो बग़दाद और नीशापुर आदि के बड़े-बड़े विद्वानों से किसी प्रकार कम न थे।
ज्ञान एवं साहित्य
इनमें एक इब्ने हय्यान थे। यह अन्दलुस के सबसे बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने साठ खण्डों में अन्दलुस का इतिहास लिखा परन्तु अब असल इतिहास नहीं मिलता, सिर्फ़ उसका सार-संक्षेप मिलता है।
अन्दलुस के सबसे बड़े लेखक इब्ने हज़्म (384 हि०/994 ई० से 456 हि०/1064 ई०) हैं। यह इतिहासकार, मुहद्दिस (हदीस के ज्ञाता) और दार्शनिक थे। इब्ने हज़्म ने इतनी किताबें लिखीं कि सिवाय तबरी के और दो-एक और लेखकों के और कोई भी लेखक उनका मुक़ाबला नहीं कर सकता। उनकी किताबों में सबसे प्रसिद्ध 'अल-मिलल वन्-निहल' है। उसमें उन्होंने सारी दुनिया के धर्मों का हाल लिखा है और बताया है कि किस धर्म में क्या ख़राबी या क्या ख़ूबी है। उनसे पहले किसी ने इस प्रकार की किताब नहीं लिखी थी।
अब्दुल मलिक बिन ज़ह्र (मृत्यु -557 हि०/1162 ई०) अन्दलुस का सबसे बड़ा चिकित्सक उसी काल में हुआ है।
अब्बासियों के हालात में हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों में सबसे बड़ा चिकित्सक 'राज़ी' था। राज़ी के बाद इस्लामी दुनिया में जिस चिकित्सक का दर्जा है, वह है इब्ने ज़ह्र। अब्दुल मलिक बिन ज़ह्र एक ऐसे ख़ानदान से था जिसमें छः पुश्त से महान चिकित्सक एवं साहित्यकार होते चले आए थे। उसका लड़का अबू बक्र (507 हि०/1113 ई० से 595 हि०/1198 ई०) भी एक बड़ा चिकित्सक, साहित्यकार और शायर हुआ है। वह याक़ूब अल-मंसूर का विशेष चिकित्सक था। उस ख़ानदान में औरतें भी उपचार करती थीं। अतः अबू बक्र की बहन और फूफी चिकित्साशास्त्र की विशेषज्ञ थीं और मंसूर के घर में औरतों का इलाज करती थीं।
इब्ने रुश्द (520 हि०/1126 ई० से 595 हि०/1198 ई०) अन्दलुस के सबसे बड़े दार्शनिक थे। पूरब में जिस प्रकार दर्शनशास्त्र में 'इब्ने सीना' ने प्रसिद्धि प्राप्त की, अन्दलुस में वैसी ही प्रसिद्धि इब्ने रुश्द ने प्राप्त की। मुवह्हिदीन के काल में वह क़ुरतुबा के क़ाज़ी थे। बाद में यूरोप की लातीनी ज़बान में उनकी किताबों के अनुवाद हुए और ये किताबें तीन सौ साल तक यूरोप के स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं।
इब्ने अरबी (560 हि०/1165 ई० से 638 हि०/1240 ई०) बहुत बड़े धार्मिक विद्वान और सूफ़ी थे। उनकी लिखी हुई किताबों में 'फ़ुसूसुल हकम' और 'फ़ुतूहाते मक्किया' आज भी बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं। वह हालाँकि अन्दलुस में पैदा हुए थे परन्तु उम्र का बड़ा भाग मिस्र एवं शाम (सीरिया) में गुज़रा और वहीं इंतिक़ाल हुआ।
इदरीसी (493 हि०/1100 ई० से 560 हि०/1165 ई०) अन्दलुस के सबसे बड़े भूगोलविद् थे। कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा मुसलमान भूगोलविद् समझते हैं। उनकी लिखी हुई भूगोल की किताब से सारी दुनिया और विशेषकर इस्लामी दुनिया के बड़े रोचक हालात मालूम होते हैं। यूरोपवालों को अफ़्रीक़ा से संबंधित बहुत-सी जानकारी पहली बार इदरीसी के भूगोल की किताब से ही हुई।
मराकश (Morocco)
क़ाहिरा, बग़दाद, ग़ज़नी और पूरब के दूसरे बड़े शहरों का हाल हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। मुवह्हिदीन के ज़माने में पश्चिम के इलाक़े में दो शहर इतनी तरक़्क़ी कर गए थे कि वे अपनी विशालता, आबादी, चमक-दमक, ज्ञान एवं कला और उद्योग-धंधे में पूरब के बड़े शहरों का मुक़ाबला करते थे। ये दोनों शहर जिनमें एक मराकश और दूसरा फ़ास (Fez) था, मुसलमानों ने ही आबाद किए थे और ये मुवह्हिदीन के काल में अपने चरम को पहुँच गए थे। मराकश 465 हि०/1072 ई० में आबाद हुआ था और आबादी के लिहाज़ से अफ़्रीक़ा में सल्तनते मुवह्हिदीन का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मुल्क-मुल्क के लोग जमा हो गए थे। अतः एक शायर लिखता है—
"मराकश में सारी दुनिया के लोग हैं और मैं नहीं समझता कि क़ियामत से पहले कभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं।"
इसी प्रकार एक इतिहासकार लिखता है—
“मुवह्हिदीन के ज़माने में मराकश में इतना अधिक पानी लाया गया कि इससे पहले कभी नहीं लाया गया था और ऐसे महल बनाए गए कि उनसे पहले किसी और बादशाह के ज़माने में नहीं बने थे। परिणामतः मराकश अति सुन्दर बन गया।"
मराकश के पीछे अटलस पहाड़ की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और सामने खजूरों के मरुद्यान शहर की सुन्दरता को और बढ़ाते थे। 'जामे कुतबिया' शहर की नाक थी और अब भी है। उसके ऊँचे मीनार से पचास-पचास मील तक ज़मीन नज़र आती थी। मीनार की चोटी पर सोने के तीन गुम्बद थे और मस्जिद के नीचे किताबों की दो सौ से अधिक दुकानें थीं जिसके कारण यह मसजिदे कुतबिया यानी किताबोंवाली मस्जिद कहलाती थी।
फ़ास (Fez)
फ़ास का शहर उत्तरी-पश्चिमी अफ़्रीक़ा में ज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र था। इसके अलावा यह शहर उद्योग-धंधे के लिहाज़ से भी अग्रणी था। मुवह्हिदीन के काल का एक इतिहासकार लिखता है—
"फ़ास को पश्चिम का बग़दाद कहा जाता है। यहाँ की जनता बुद्धिमान और साहसी है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई शहर फ़ास जैसा होगा जहाँ विलासिता के सामान और जीवन के साधन इतने अधिक पाए जाते हों। शहर के चारों ओर हरियाली है, पानी और पेड़ इसे हर और से घेरे हुए हैं और आस-पास नहरें और नदियाँ बह रही हैं। शहर में पानी से चलनेवाली तीन सौ चक्कियाँ हैं। यहाँ भारत की सुगंधित लकड़ी के अलावा और किसी चीज़ को बाहर से लाकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फ़ास को अपनी ज़रूरत के लिए किसी और शहर के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता।"
फ़ास का शहर 192 हि०/808 ई० में आबाद हुआ था और आज भी पश्चिम या मुल्क मराकश का सबसे बड़ा बौद्धिक और वैचारिक केन्द्र है। उत्तरी अफ़्रीक़ा की सबसे बड़ी मस्जिद 'जामे क़रविईन' इस शहर में है। मस्जिद की बुनियाद इदरीसी दौर में पड़ी थी परन्तु वर्तमान इमारत के अधिकतर भाग का संबंध ग्यारहवीं ईस्वी शताब्दी से है। यह मस्जिद क़ाहिरा के 'जामे अज़हर' की तरह एक शैक्षणिक विद्यालय भी है बल्कि जामे अज़हर के बाद इस्लामी दुनिया का सबसे प्राचीन शैक्षणिक केन्द्र है और उत्तरी एवं पश्चिमी अफ़्रीक़ा में आज भी इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है।
ख़ानदाने मराबतीन की हुकूमत
(453 हि०/1061 ई० से 541हि०/1147 ई०)
1. यूसुफ़ विन ताशफ़ीन - 453 हि०/1061 ई० से 500 हि०/1107 ई०
2. अली बिन यूसुफ़ ताशफ़ीन - 500 हि०/1107 ई० से 537 हि०/1143 ई०
3. ताशफ़ीन बिन अली - 537 हि०/1143 ई० से 541 हि०/1147 ई०
ख़िलाफ़ते मुवह्हिदीन
(524 हि०/1130 ई० से 667 हि०/1269 ई०)
1. अब्दुल मोमिन - 524 हि०/1130 ई० से 558 हि०/1163 ई०
2. यूसुफ़ - 558 हि०/1163 ई० से 580 हि०/1184 ई०
3. याक़ूब अल-मंसूर - 580 हि०/1184 ई० से 595 हि०/1199 ई०
4. मुहम्मद अन-नासिर - 595 हि०/1199 ई० से 611 हि०/1214 ई०
5. यूसुफ़ मुस्तंसिर - 611 हि०/1214 ई० से 620 हि०/1223 ई०
इसके बाद मुवह्हिदीन का पतन शुरू हो गया।
ज़ल्लाक़ा की जंग - 479 हि०/1086 ई०
अल-अरक की जंग - 591 हि०/1195 ई०
अल-अक़्क़ाब की जंग - 609 हि०/1212 ई०
अध्याय-20
अन्दलुस का विनाश : एक सभ्यता का अन्त
मुवह्हिदीन के बाद अन्दलुस में मुसलमानों का पूरी तरह पतन शुरू हो गया। उत्तर में क़शताला को ईसाई हुकूमत जिसने मराबतीन और मुवह्हिदीन से घमासान लड़ाइयाँ की थीं अब और अधिक शक्तिशाली हो गई। मुसलमान जमकर उसका मुक़ाबला नहीं कर सके और क़ुरतुबा, इशबीलिया और बलंसिया जैसे महान नगर जो अन्दलुस में इस्लामी सभ्यता एवं संस्कृति के सबसे बड़े केन्द्र थे, एक-एक करके मुसलमानों के हाथ से निकल गए। अब मुसलमानों की हुकूमत मुल्क के दक्षिणी-पूर्वी किनारे में छोटे से क्षेत्र में सीमित होकर रह गई जिसका क्षेत्रफल सात हज़ार वर्गमील से अधिक नहीं था। ग़रनाता (Garnada) इस हुकूमत का प्रधान स्थल (राजधानी) था और माल्क़ा एवं अल-मरया उसके बड़े बंदरगाह थे।
ग़रनाता की यह हुकूमत जिसे बनू अहमर (636 हि०/1238 ई० से 898 हि०/1492 ई०) की हुकूमत भी कहते हैं, हालाँकि क़शताला की हुकूमत के मुक़ाबले में बहुत छोटी थी, परन्तु इसके बावजूद वह ढाई सौ साल तक दुश्मनों का बड़ी कामयाबी से मुक़ाबला करती रही और अन्दलुस के मुसलमानों के लिए एक पनाहगाह बन गई। ग़रनाता की हुकूमत हालाँकी बहुत छोटी थी, परन्तु उसका यह कारनामा गर्व करने योग्य है कि उसने मुसलमानों और इस्लामी सभ्यता को यूरोप के संकीर्ण, अत्याचारी और वहशी दुश्मनों के हाथों ढाई सौ साल तक तबाह होने से बचाए रखा।
मुसलमान अन्दलुस के ईसाई क्षेत्रों से निकलकर ग़रनाता में आबाद होने लगे जिसके कारण ग़रनाता और दूसरे शहर बहुत जल्द ज्ञान एवं कला और उद्योग-धंधों के केन्द्र बन गए। ग़रनाता की आबादी उस ज़माने में चार लाख तक पहुँच गई थी। उसके ज्ञान एवं कला और उद्योग-धंधों की ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गई थी और वहाँ का तिजारती सामान यूरोप और इस्लामी दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में जाता था।
वास्तुकला में ग़रनाता के बादशाहों और कारीगरों की सबसे शानदार यादगार अल-हमरा के महल हैं। ये महल और उसके बाग़ जो 'जन्नतुल-आरिफ़' कहलाते हैं अन्दलुस के मुलसमानों की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना हैं। भारत की प्राचीन इमारतों में जो हैसियत ताजमहल को प्राप्त है बिलकुल वही हैसियत अन्दलुस में ‘अल-हमरा' को प्राप्त है और उसे देखने के लिए आज भी सारी दुनिया से पर्यटक ग़रनाता आते हैं और उसके बनानेवाले कारीगरों एवं इंजीनियरों की प्रशंसा करते हुए वापस जाते हैं।
पंद्रहवीं शताब्दी में ग़रनाता के शाही ख़ानदान के लोग आपस में लड़ने लगे जिससे मुसलमानों की शक्ति कमज़ोर हो गई और ईसाइयों के हौसले बढ़ गए।
अबू अब्दुल्लाह यहाँ का आख़िरी बादशाह हुआ है। उसके काल में क़शताला की ईसाई हुकूमत ने बड़ा ज़ोर पकड़ा और शहर ग़रनाता का घेराव कर लिया। जब इस घेराव को महीना भर गुज़र गया और शहर के लोगों के पास खाने-पीने को कुछ नहीं रहा तो अबू अब्दुल्लाह ने ईसाइयों की अधीनता स्वीकार करने का फ़ैसला कर किया। बादशाह का यह फ़ैसला देखकर ग़रनाता की फ़ौज के सिपहसालार मूसा ने इस फ़ैसले का विरोध किया और कहा—
“हमारा अधीनता स्वीकार करना बड़े अपमान की बात है। हमें दुश्मन का मुक़ाबला जारी रखना चाहिए। यदि हमें कामयाबी नहीं मिली तो हम जंग के मैदान में इज़्ज़त की मौत तो मर सकते हैं।"
परन्तु अबू अब्दुल्लाह ने अपने सिपहसालार का कहना न माना और ईसाई बादशाह फ़रडिनेण्ड के आगे हथियार डाल दिया। मूसा ने जब यह देखा तो वह अकेला घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला। दुश्मनों पर आक्रमण किया और बहुत-से सिपाहियों को मौत के घाट उतारा और जब ज़ख़्मों से चूर हो गया तो नदी में कूद पड़ा और पानी में डूब गया। ईसाई उसकी लाश पर भी क़ब्ज़ा नहीं कर सके। उसके इस साहस और वीरता के कारण मूसा का नाम इतिहास में अमर हो गया और लोग आज तक उसका नाम इज़्ज़त और सम्मान से लेते हैं।
अबू अब्दुल्लाह ने इसके बाद शहर को ईसाई हुकूमत के हवाले कर दिया और ख़ुद मराकश चला गया। जब वह ग़रनाता से कुछ मील की दूरी पर एक पहाड़ पर पहुँचा तो ग़रनाता पर, जो कई सौ साल तक मुसलमानों के क़बज़े में रहा, हसरत भरी निगाह डाली और रोने लगा। अबू अब्दुल्लाह की माँ साथ थी। उसने जब अपने बेटे को रोते देखा तो कहा—
“जब तुम मर्दों की तरह अपने शहर को न बचा सके तो औरतों की तरह रोने से क्या फ़ायदा।"
यह घटना 898 हि०/1492 ई० की है। इसके बाद अन्दलुस पर मुसलमानों की हुकूमत कभी क़ायम न हुई।
इस्लामी अन्दलुस के इस अन्तिम काल में ग़रनाता में कई विद्वान और लेखक पैदा हुए। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध लिसानुद्दीन इब्ने ख़तीब (1313 ई० से 1374 ई०) हैं। वह कई साल तक ग़रनाता के प्रधानमंत्री भी रहे। वह एक महान चिन्तक, इतिहासकार और शायर थे। इब्ने ख़तीब ने अपनी ज़िन्दगी में साठ किताबें लिखीं जो साहित्य, शायरी, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब 'अल अहाता फ़ी अख़बारि ग़रनाता' है। यह कई खण्डों में है और ग़रनाता का सबसे पूर्ण और विस्तृत इतिहास है। इसमें तमाम अलिमों और प्रसिद्ध लोगों के हालात उल्लिखित हैं।
अन्दलुस से मुसलमानों का निष्कासन
ईसाइयों ने अन्दलुस पर क़बज़ा करने के बाद मुसलमानों पर बहुत ज़ुल्म किया। अरबी ज़बान पढ़ना और बोलना जुर्म (अपराध) घोषित कर दिया। लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया। हज़ारों मुसलमानों को जिन्होंने ईसाइयत क़बूल नहीं की क़त्ल कर दिया गया अथवा ज़िन्दा जला दिया गया। कई लाख मुसलमान मुल्क से निकाल दिए गए या हिजरत कर गए। अनुमान लगाया गया है कि निष्कासित होनेवाले मुसलामानों की तादाद तीस लाख थी। शेष आबादी ने जान के भय से ईसाई धर्म क़बूल कर लिया। अन्दलुस में जहाँ आठ सौ साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी 1610 ई० के बाद एक मुसलमान भी शेष नहीं बचा। और आज वहाँ मुसलमानों के शासन काल में बनाई हुई कुछ इमारतों के अलावा और कुछ नहीं। अन्दलुस में मुसलमानों के अन्त की दास्तान बहुत दर्दनाक है। इसकी मिसाल मानव इतिहास में नहीं मिलती।
अध्याय-21
यूरोप के उस्ताद
अन्दलुस की सरज़मीन से हालाँकि मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया और आज वहाँ ख़ुदा और उसके रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नाम लेनेवाला कोई नहीं, परन्तु मुसलमानों ने अपने आठ सौ साल के शासन काल में वहाँ ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो इतिहास में हमेशा याद किए जाएँगे। अन्दलुस के दो हज़ार वर्ष के इतिहास में वहाँ कई क़ौमों ने हुकूमत की। सबसे पहले क़रताजनावालों की हुकूमत क़ायम हुई। उसके बाद कई सौ साल तक रूमियों ने डंका बजाया। फिर क़ौती या गोथा लोगों के हाथ में हुकूमत की बागडोर आई। उसके बाद मुसलमान आए और उनके जाने के बाद वहीं के प्राचीन ईसाई लोगों ने अपनी हुकूमत क़ायम की, जो अब तक है। इन तमाम क़ौमों ने बारी-बारी मुल्क की सेवा की और बहुत-से कारनामे अंजाम दिए, परन्तु वास्तविकता यह है कि इनमें से किसी क़ौम के कारनामे इस्लामी काल के कारनामों से अधिक शानदार नहीं और किसी काल में अन्दलुस को वह ख़ुशहाली प्राप्त नहीं हुई जो इस्लामी काल में प्राप्त हुई। पूरे इतिहास में केवल इस्लामी काल ही ऐसा है कि जब अन्दलुस के लोगों ने दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया, और केवल यही वह काल है जिसमें अन्दलुसवालों ने यूरोप में ज्ञान एवं कला की रौशनी फैलाई। अन्दलुस के इतिहास के किसी काल को यदि हम स्वर्णिम काल कह सकते हैं, तो वह केवल “इस्लामी काल" है।
अन्दलुस हालाँकि छोटा-सा देश था परन्तु जहाँ तक ज्ञान एवं कला और सभ्यता व संस्कृति का सम्बन्ध है यह देश इस्लामी काल में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं था। यहाँ के दीनी आलिमों (धार्मिक विद्वानों) में इब्ने हज़्म, इब्ने अब्दुल बर्र और इब्ने अरबी, दार्शनिकों में इब्ने तूफ़ैल और इब्ने रुश्द, चिकित्सकों में ज़ुहरावी और इब्ने ज़ुहर और साहित्यकारों एवं इतिहासकारों में इब्ने अब्दे रब्बिही और ख़तीब और शायरों में इब्ने ज़ैदून और इब्ने अम्मार न केवल इस्लामी दुनिया के महानतम विद्वानों, दार्शनिकों, चिकित्सकों, साहित्यकारों, इतिहासकारों और शायरों में से हैं, बल्कि इस्लामी इतिहास में सिवाय इराक़ और मावराउन-नहर के किसी और देश ने जो अन्दलुस की तरह छोटा हो, इतनी बहुलता से ज्ञान एवं कला के विशेषज्ञ पैदा नहीं किए। दुनिया के शेष दूसरे देशों में भी इसकी मिसालें कम ही मिलेंगी।
दुनिया में हवाई जहाज़ बनाने की सबसे पहली कोशिश इस्लामी अन्दलुस ही के एक वैज्ञानिक अब्बास इब्ने फ़रनास ने की। उसका हवाई जहाज़ थोड़ी ऊँचाई तक उड़ा भी था, परन्तु फिर गिर गया। इब्ने फ़रनास बहुत मेधावी वैज्ञानिक था। उसने अपने घर में एक कृत्रिम आसमान भी बनाया था जिसमें सूरज, चाँद और सितारे बनाए गए थे। उसने पत्थर से शीशा तैयार करने की विधि का आविष्कार किया और छाया की मदद के बिना समय मालूम करने के लिए एक यंत्र का भी अविष्कार किया था।
इसी प्रकार मुवह्हिदीन के ज़माने में इशबीलिया के एक कृषि विशेषज्ञ इब्ने अव्वाम ने कृषि को विकास देने, क़लमें लगाने और ज़मीन को काश्तकारी के लिए बेहतर बनाने के ऐसे-ऐसे तरीक़े अपनी किताब में लिखे हैं जिनका दुनिया को अब जाकर ज्ञान हुआ है।
इस्लामी अन्दलुस के वासियों ने पहली बार चावल, ज़ाफ़रान, नारंगी, नींबू, अंगूर, ख़रबूज़ा, केले और पीले गुलाब, चंबेली, रूई और गन्ने की खेती अन्दलुस में की। उस समय तक ये चीज़ें अन्दलुस या यूरोप में पैदा नहीं हुई थीं। इन चीज़ों की खेती करना यूरोप के कई देशों ने अन्दलुस ही से सीखा।
यह तो सब जानते हैं कि आजकल मुसलमानों के मुक़ाबले में यूरोप और अमेरिका की क़ौमे ज़्यादा विकसित हैं। उनके पास धन-दौलत भी ज़्यादा है, ज्ञान भी ज़्यादा है, उनके शहर भी हमारे शहरों के मुक़ाबले में बहुत सुन्दर हैं और उनकी इमारतें और उन इमारतों का साज़ो सामान उत्तम कोटि का होता है। परन्तु यह कम लोगों को मालूम है कि मुसलमानों के उत्थान के ज़माने में यह मामला उलटा था। मुसलमानों के पास ज्ञान था, दौलत थी। उनके पास बड़े-बड़े और सुन्दर शहर थे। वह पाक (पवित्र) और साफ़-सुथरे रहते थे। इसके विपरीत यूरोपवाले अज्ञानी थे, निर्धन थे और जिस प्रकार आज मुसलमान अंग्रेज़ी ज़बान के माध्यम से अपना ज्ञान और अपनी मालूमात बढ़ाने और उच्च शिक्षा के लिए यूरोप और अमेरिका जाते हैं उसी प्रकार मुसलमानों के उत्कर्ष काल में यूरोप के ईसाई ज्ञान अर्जित करने के लिए अरबी ज़बान सीखते थे और इस्लामी देशों में आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अन्दलुस का मुल्क चूँकि यूरोप के दूसरे देशों के निकट था इसलिए उन्होंने सबसे अधिक लाभ अन्दलुस के आलिमों, मदरसों एवं पुस्तकालयों से उठाया।
एक मुसलमान इतिहासकार क़ज़दीनी लिखता है—
"डेनमार्क के लोग बिलकुल वहशी हैं, नंगे रहते हैं और चमड़े के टुकड़ों से शरीर के विशेष अंगों (गुप्तांगों) को छुपाते हैं।"
उन देशों को छोड़कर जो इस्लामी दुनिया से मिले हुए थे, अधिकतर देशों का यही हाल था।
पेरिस और लंदन में बाँस और लकड़ी के घर बनाए जाते थे, जिन्हें मिट्टी और भूसे से लीप दिया जाता था। लोग बिस्तर के बारे में नहीं जानते थे। भूसा और पयाल बिस्तर का काम देता था, जानवरों की आंतें और कूड़ा-करकट घरों के सामने लाकर डाल देते थे।
जब लोगों की सभ्यता एवं संस्कृति की यह हालत हो तो स्पष्ट है कि ज्ञान से उनका दूर का भी वास्ता नहीं हो सकता। अतः उत्तरी यूरोप के लोगों के संबंध में तो मुसलमानों में यह आम धारणा थी कि वे लोग प्राकृतिक रूप से मूर्ख हैं और अत्यधिक ठण्ड के कारण उनकी बुद्धि क्षीण हो गई है।
अन्दलुस के दो प्रसिद्ध विद्वानों इब्ने साइद और इब्ने ख़लदून ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं।
इब्ने साइद लिखते हैं—
“जो क़ौमें उदाहरणतः सक़ालिया (सक़लिया टापू की क़ौम) और बुलग़ार (बुलग़ारिया की क़ौम) आदि जो सुदूर उत्तरी क्षेत्र में आबाद हैं, जहाँ सूरज से दूरी के कारण हवा में ठण्डक और वातावरण में गंदगी पैदा हो गई है, उनके स्वभाव सर्द (ठण्डे) और मस्तिष्क गठिल हो गए हैं। यही कारण है कि उनके शरीर मोटे हो गए, रंग सफ़ेद हो गया और बाल लटक गए। अतः यह क़ौमें सूक्ष्मदर्शन और बुद्धि की तेज़ी से वंचित रहीं और अज्ञानता एवं मूर्खता इनपर सवार हो गई और ये लोग इनसानों से अधिक जानवरों से प्रतीत होते हैं।"
यह बिलकुल ऐसा ही विचार है जैसा कि आजकल यूरोप की प्रगति के कारण लोगों में यह प्रचलित हो गया है कि एशिया के लोग गर्म देश के रहनेवाले हैं इसलिए सुस्त एवं आलसी होते हैं और उनके मस्तिष्क यूरोपवालों की तरह काम नहीं करते। वास्तविकता यह है कि ये सारे विचार ग़लत हैं। यूरोप की प्रगति ने इब्ने साइद और इब्ने ख़लदून के विचार को ग़लत साबित कर दिया और मुसलमानों और एशिया की क़ौमों का विगत उत्थान इस बात का प्रमाण है कि यूरोपवालों का भी एशियावालों के बारे में इस प्रकार की अवधारणा ग़लत है। हर क़ौम की प्रगति और विकास का एक समय होता है और जब किसी क़ौम का भाग्य चमकता है तो न सर्दी उसकी राह में रुकावट बनती है और न गर्मी।
क़ुरतुबा का शहर यूरोपवालों के लिए उस ज़माने में ऐसा ही था जैसा इस्लामी देशों के नागरिकों के लिए आजकल यूरोप के मुल्क और न्यूयार्क आदि हैं। क़ुरतुबा की आबादी अपने उत्थान के ज़माने में पंद्रह लाख के लगभग थी। शहर 24 मील लम्बा और 7 मील चौड़ा था और वादियुल-कबीर नदी के किनारे-किनारे फैला हुआ था। इस शहर में दो लाख साधारण मकान थे और साठ हज़ार महल, कोठियाँ और बड़े मकान। अस्सी हज़ार दुकानें, तीन हज़ार आठ सौ मस्जिदें और सात सौ स्नानगृह थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा शहर बड़ी अजीबो ग़रीब चीज़ समझी जाती थी। शहर की सड़कें पक्की थीं। गंदे पानी की निकासी के लिए भूमिगत नालियाँ थीं। चौराहों पर फ़व्वारे लगे हुए थे। रात के समय रास्तों पर रौशनी की व्यवस्था होती थी, मकानों और सड़कों की रौशनी की अधिकता के कारण लोग दस-दस, पंद्रह-पंद्रह मील तक रास्ता चलते थे।
एक इतिहासकार लिखता है कि—
"क़ुरतुबा आबादियों का सरताज, हर किसी को प्रिय, अपेक्षित, नेक और धर्मपरायण लोगों का केन्द्र, ज्ञान का स्रोत और इस्लाम का घर है। दुनिया भर की बुद्धि सिमटकर यहाँ जमा हो गई हैं। उसके क्षितिज से दुनिया के तारे निकले हैं, विख्यात लोग पैदा हुए और साहित्य के क्षेत्र में गद्य एवं पद्य शहसवारों के घोड़े दौड़े और उच्च कोटि की किताबें यहीं लिखी गईं।"
क़ुरतुबा के लोग बड़े सुसभ्य एवं सुसंस्कृत होते थे। लिबास की ख़ुशनुमाई, दीनदारी और नमाज़ की पाबन्दी में मशहूर थे। वे जहाँ कहीं शराब के बर्तन देखते, उन्हें तोड़ डालते थे। फ़ौजी ज्ञान एवं कला में उन्हें गर्व प्राप्त था।
पूरी दुनिया में सिवाय बग़दाद के कोई शहर क़ुरतुबा का मुक़ाबला नहीं कर सकता था। क़ुरतुबा तो क़ुरतुबा था, यूरोप में कोई शहर इशबीलिया, बलंसिया, ग़रनाता और सरक़स्ता के बराबर नहीं था। उस ज़माने के लंदन और पेरिस छोटे-छोटे शहर थे। उनकी सड़कें कच्ची होती थीं। गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता था। मकान घास-फूस के थे। लोग खिड़कियों में शीशे के स्थान पर काग़ज़ को तेल में डुबोकर लगा लेते थे ताकि आरपार दिख सके।
उस ज़माने में यूरोप में सिवाय पादरियों और कुछ अमीरों (उच्च पदस्थ अधिकारियों) के कोई लिखना-पढ़ना नहीं जानता था, परन्तु अन्दलुस का हर मुसलमान पढ़ा-लिखा होता था। फ़्रांस के बादशाह के पुस्तकालय में केवल 6-7 सौ किताबें थीं। इसके विपरीत क़ुरतुबा में अनगिनत लोगों के पास निजी पुस्तकालय थे, जिनमें हज़ारों किताबें थीं, और शाही पुस्तकालय में तो चार लाख किताबें थीं। घर में निजी पुस्तकालय रखना और किताबें जमा करना उस ज़माने में एक प्रकार का फ़ैशन बन गया था। हर धनी व्यक्ति, चाहे वह किताबों को पढ़ और समझ सकता हो या नहीं, अपने घर में पुस्तकालय ज़रूर रखता था, ताकि लोग जब उसकी चर्चा करें तो गर्व से कह सकें कि उसके पुस्तकालय में वह किताब है जो किसी और के पास नहीं।
एक बार क़ुरतुबा के एक नागरिक हरमी को एक किताब की बहुत ज़रूरत थी। उसने इसकी तलाश में किताबों के बाज़ारों को छान मारा तब जाकर एक दिन यह किताब मिली, परन्तु उसका एक ग्राहक पहले से मौजूद था जो उस समय वहाँ उपस्थित नहीं था। हरमी ने उस किताब की क़ीमत बढ़ाकर देनी चाही, परन्तु पहले ख़रीदार ने और क़ीमत बढ़ा दी। इस प्रकार दोनों पक्ष की ओर से किताब की क़ीमत रोज़ बढ़ती रही। अन्ततः हरमी ने तंग आकर दुकानदार से कहा कि मुझे तुम दूसरे ख़रीदार से मिलवा दो। सम्भव है कि हम दोनों में समझौता हो जाए। दुकानदार उसे उस व्यक्ति के पास ले गया। यह एक धनी व्यक्ति था। हरमी ने समझा कि वह कोई बड़ा आलिम है इसलिए उसे फ़क़ीह यानी मौलवी साहब कहकर सम्बोधित किया। इसपर उस व्यक्ति ने कहा—
“मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि इस किताब के अन्दर क्या है। मैंने तो केवल उसकी लिखावट देखी है, और किताब की सुन्दरता देखकर प्रभावित हुआ हूँ। मैंने एक पुस्तकालय बनाया है। इसमें अच्छी-अच्छी किताबें जमा की हैं ताकि अपने साथियों में उसके कारण प्रतिष्ठा एवं ख्याति अर्जित करूँ। इसलिए आप अधिक क़ीमत न बढ़ाएँ। मेरे पास इतना धन है कि किसी भी क़ीमत पर किताब को ख़रीद सकता हूँ।"
यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उस ज़माने में आजकल की तरह छापेख़ाने (प्रेस) नहीं थे। लोगों को हाथ से किताबें लिखनी पड़ती थीं। परन्तु ज्ञान प्राप्त करने के शौक़ ने इन तमाम कठिनाइयों पर क़ाबू पा लिया था और किताबों का कारोबार बाक़ी इस्लामी दुनिया की तरह अन्दलुस में भी इतना तरक़्क़ी कर गया था कि हज़ारों लोगों का रोज़गार किताबों के लिखने और बेचने पर निर्भर था। कहते हैं कि केवल क़ुरतुबा में बीस हज़ार लोग किताबों का कारोबार करते थे।
किताबों के लिए काग़ज़ एक ज़रूरी चीज़ है। उस ज़माने में सिवाय चीन और इस्लामी दुनिया के और किसी देश के लोग काग़ज़ बनाना नहीं जानते थे। अन्दलुस में रूम सागर के तट पर बंदरगाह बलंसिया के निकट शहर 'शातिबा' (Jativa) काग़ज़-निर्माण का केन्द्र था। यहाँ के कारख़ानों का बना हुआ काग़ज़ अन्दलुस और सारे यूरोप को जाता था। बाद में यूरोपवालों ने यहाँ से काग़ज़ बनाना सीखा। फ़्रांस में सबसे पहले 1187 ई० में, जर्मनी में 1320 ई० में और इंग्लैण्ड में 1494 ई० में, काग़ज़ बनाने का उद्योग शुरू हुआ। एक अमेरिकी लेखक लिखता है—
"उस ज़माने में क़ुरतुबा यूरोप का बौद्धिक केन्द्र था। ईसाई यूरोप के विद्वान शिक्षा प्राप्त करने और रिसर्च करने के लिए इस्लामी अन्दलुस का रुख़ करते थे और अन्ततः उन्हीं लोगों के माध्यम से अरबों के बहुत-से ज्ञान फ़्रांस और इटली पहुँच गए।" (तहज़ीब का माज़ी और हाल, पृ० 419)
यूरोप के जिन प्रसिद्ध लोगों ने अन्दलुस आकर ज्ञानार्जन किया उनमें रूम के पोप स्नावेस्टर द्वितीय (940-1003) भी हैं। वे फ़्रांस के रहनेवाले थे। बड़े होकर अन्दलुस में शिक्षा प्राप्त की। विज्ञान, गणित और संगीत पर कई किताबें लिखीं। अन्त में 999 ई० में रूम के पोप चुने गए। अंकों, शून्य और दशमलव का इस्तेमाल सीखकर उन्होंने यूरोप में उन चीज़ों को प्रचलित किया। जब वे यूरोप वापस पहुँचे तो उस्तरलाब (नक्षत्र विज्ञान) और गणित के उपयोग में असाधारण योग्यता देखकर लोग यह कहने लगे कि उन्होंने यह चीज़ें शैतान से सीखी हैं।
मुसलमानों के विकास काल में यूरोप के लोग कुछ तो अपनी अज्ञानता के कारण और कुछ अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक तादाद में अन्दलुस नहीं आते थे, परन्तु जब धीरे-धीरे उनपर मुसलमानों का प्रभाव पड़ा और उनमें ज्ञान का महत्त्व पैदा हुआ और 1085 ई० में शहर तुलैतिला पर ईसाइयों का क़बज़ा हो गया तो यूरोप के हर क्षेत्र से विद्वान तुलैतिला आने लगे और यहाँ कि अरबी किताबों से फ़ायदा उठाने लगे।
यूरोप का एक इतिहासकार लिखता है—
“क़शताला और ल्यून के ईसाई हुक्मरान अलफ़ान्सो षष्ठम (1065-1109) का दरबार इस्लामी सभ्यता का उसी प्रकार केन्द्र बन गया था, जिस प्रकार दो सौ साल बाद पिलरमू में फ़्रेडरिक द्वितीय [अन्दलुस की तरह सक़लिया टापू यानी सिसली भी यूरोप में मुसलमानों की सभ्यता का एक बड़ा केन्द्र था। इस टापू पर मुसलमानों ने लगभग ढाई सौ साल तक (216 हि०/831 ई० से 483 हि०/1090 ई०) हुकूमत की। उत्तरी यूरोप की एक क़ौम ने जो 'नारमन' कहलाती थी उस टापू से मुसलमानों की हुकूमत समाप्त कर दी। नारमन ने हालाँकि उस काल में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, परन्तु नारमन बादशाहों के दरबार में काफ़ी समय तक मुसलमानों की सभ्यता का प्रभाव रहा। उन बादशाहों में एक रॉजर द्वितीय (1101 ई० से 1154 ई०) हुआ है। उसका मुसलमानों के साथ इतना अच्छा सुलूक था कि ईसाइयों में यह प्रसिद्ध था कि वह मुसलमान हो गया है। उसने प्रसिद्ध भूगोल-विद् इदरीसी (493 हि०/1099 ई० से 560 हि०/1153 ई०) को अफ़्रीक़ा से बुलाकर दुनिया के भूगोल पर एक किताब लिखवाई और दुनिया का एक नक़्शा तैयार करवाया। वर्तमान काल से पहले यह दुनिया का सबसे सही नक़्शा था। इदरीसी की किताबों का 1619 ई० में यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और उसके माध्यम से यूरोपवालों को पहली बार एशिया और विशेषकर अफ़्रीक़ा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई।
एक और नारमन हुक्मरान फ़्रेडरिक द्वितीय (1194 ई० से 1250 ई०) मुसलमानों जैसा लिबास पहनता था और दरबार में मुसलमान चिकित्सक, विद्वान और सलाहकार रखता था। उसके ज़माने में इस्लामी सभ्यता का इतना प्रभाव था कि ईसाई औरतें भी पर्दा करती थीं। उसके ज़माने में अरबी की बहुत-सी किताबों का लातीनी भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनमें एक प्रसिद्ध किताब राज़ी की 'हादी' है। बाद में ये किताबें सारे यूरोप में फैल गईं। उस ज़माने में दक्षिणी इटली के शहर सलोनो में अरबों के सहयोग से एक चिकित्सा विद्यालय (मेडिकल कॉलेज) 1070 ई० में क़ायम हुआ जो यूरोप में पहला मेडिकल कॉलेज था। यहाँ मुसलमान चिकित्सकों की किताबें पढ़ाई जाती थीं।] का दरबार इस्लामी सभ्यता का केन्द्र बना। उसके ज़माने में तुलैतिला की दर्सगाहों में यूरोप के सभी क्षेत्रों से यहाँ तक कि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड से विद्वान खिंच-खिंचकर चले आते थे।"
मुसलमानों के ज्ञान को संरक्षण देने में क़शताला का एक दूसरा हुक्मरान अलफ़ांसो द्वितीय (1252 ई० से 1284 ई०) सबसे आगे बढ़ गया। उसके काल में बहुत-सी अरबी किताबों का हिस्पानवी और लातीनी भाषाओं में अनुवाद हुआ और अरबी किताबों की मदद से लातीनी भाषाओं में भी किताबें लिखी गईं।
मुलसमानों के इस प्रभाव का यह परिणाम हुआ कि 1230 ई० में अन्दलुस के शहर सलामंका में ईसाइयों ने एक यूनीवर्सिटी क़ायम की जो ईसाई-यूरोप की पहली यूनीवर्सिटी समझी जाती है।
तुलैतिला में अनुवाद का काम पूरे दो सौ साल तक जारी रहा। अनुवाद करने के उद्देश्य से यूरोप के हर हिस्से से विद्वान इस शहर में आते थे और अरबी से लातीनी ज़बान में, जो उस समय यूरोप की बौद्धिक ज़बान थी, अनुवाद करते थे। उनमें निम्न लिखित अनुवादक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं:
1. जरार्ड क़रामूनी - (1114 ई० 1187 ई०) - इटली का रहनेवाला था। उसने तुलैतिला आकर इतनी अधिक अरबी किताबों का लातीनी ज़बान में अनुवाद किया कि उसे अरबी ज्ञान का प्रथम पुरुष कहा जाने लगा। उसने जिन प्रसिद्ध लेखकों की किताबों का अनुवाद किया उनमें किन्दी, फ़ाराबी, इब्ने-सीना और ज़ुहरावी का नाम उल्लेखनीय है।
2. एडलार्ड आफ़ बाथ - बारहवीं शताब्दी का एक अंग्रेज़ पर्यटक, जो अनुवादक और लेखक गुज़रा है, जरार्ड का समकालीन था। उसने अन्दलुस आकर ख़्वारिज़्मी और दूसरे लेखकों की किताबों का अनुवाद किया।
3. माइकल स्काट - (1175 ई० से 1234 ई०) - अंग्रेज़ था। तुलैतिला में अरबी सीखी और फ़्रेडरिक द्वितीय के दरबार में अरबी किताबों का लातीनी में अनुवाद किया। बाद में बादशाह के आदेश से ये किताबें यूरोप के सभी स्कूलों तक पहुँचा दी गईं। नक्षत्रविज्ञान और रसायनशास्त्र आदि पर उसने जो किताबें लिखीं उसके कारण यूरोप के लोग पोप सिलवेस्टर की तरह उसे भी जादूगर समझते थे।
इन अनुवादों के कारण यूरोप में ज्ञान एवं कला का विस्तार हुआ और मुसलमान वहाँ के बौद्धिक जीवन पर ऐसे छा गए कि इब्ने रुशद की दर्शन की किताबें और इब्ने सीना की चिकित्सा की किताबें तीन सौ साल तक यूरोप की यूनीवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रहीं।
यूरोप में उस ज़माने में इतनी अज्ञानता थी कि जो कोई गणित, खगोलशास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र या विज्ञान की समस्याएँ हल करता था तो लोग उसे जादूगर समझते थे। पोप सिलवेस्टर और माइकल स्कॉट की तरह एक और अंग्रेज़ दार्शनिक एवं लेखक रॉजर बेकन (1214 ई० – 1294 ई०) पर भी यही इलज़ाम था। उसने अरबी किताबें पढ़ने के बाद जो किताबें लिखीं उनका विरोध किया गया और दस साल तक वह पेरिस में क़ैद रहा।
1511 ई० में हिस्पानिया की हुकूमत ने अरबी किताबों को जला देने का आदेश दिया और इस प्रकार लाखों किताबें बरबाद कर दी गईं। केवल ग़रनाता में अस्सी में हज़ार किताबें जलाई गईं। कुछ किताबें जो जलने से बच गईं हिस्पानिया में एस्कोरियाल (Escorial) के पुस्तकालय में अब भी सुरक्षित हैं।
ज्ञान एवं कला की तरह अन्दलुस के मुसलमानों ने कृषि और उद्योग को भी ख़ूब विकसित किया। चावल और गन्ना उन्होंने पहली बार उपजाया और यहाँ से वे यूरोप में फैला। कृषि के तरीक़े और नहरों द्वारा सिंचाई वे ख़ूब जानते थे। यह प्रणाली फ़्रांसीसियों ने उनसे सीखा।
मेक्स म्यूहोफ़ लिखता है—
"अन्दलुस के लेनिन नामक कपड़े ने बड़ी ख्याति प्राप्त की और क़ुरतुबा का रेशम दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। अन्दलुस में तैयार होनेवाले चमड़े के सामान, हथियारों, शीशा और मशजर कपड़ों का यूरोप में कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता था।" —तहज़ीब का माज़ी और हाल (अंग्रेज़ी संस्करण)
“इस प्रकार यूरोप की सरज़मीन में, जो बौद्धिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से बंजर थी, सैकड़ों अरबी किताबों के अनुवाद हो गए और जिस प्रकार वर्षा से बंजर ज़मीन हरी-भरी और उर्वर बन जाती है, वही प्रभाव इन अनुवादों से यूरोप पर हुआ।" —तहज़ीब का माज़ी और हाल, पृष्ठ-351 (अंग्रेज़ी संस्करण)
अब यदि हम अन्दलुस के मुसलमानों को यूरोप का उस्ताद कहें तो आप ख़ुद ही बताइए कि यह सही होगा या नहीं।
यह है संक्षिप्त इतिहास यूरोप में ज्ञान एवं कला और विज्ञान की रौशनी फैलने का। हालाँकि यूरोप को सभ्य बनाने का गर्व पूरी इस्लामी दुनिया को प्राप्त है, परन्तु अन्दलुस चूँकि यूरोप से सबसे निकट था इसलिए यूरोपवालों ने सबसे अधिक लाभ भी वहीं से उठाया। और इस प्रकार अन्दलुस के मुसलमान निश्चय ही 'यूरोप के उस्ताद' कहे जाने के अधिकारी हैं।
अध्याय-22
आग और ख़ून का सैलाब
ख़्वारिज़्म शाही सल्तनत
सलजूक़ियों के पतन के बाद इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग में जो हुकूमतें क़ायम हुईं उनमें कारनामों के आधार पर हालाँकि शाम (Syria)) और मिस्र (Egypt) की ज़ंगी और अय्यूबी और हरात की ग़ौरी हुकूमत अधिक महत्त्वपूर्ण है, परन्तु क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी हुकूमत ख़्वारिज़्म की थी। इस हुकूमत की बुनियाद ख़्वारिज़्म के सलजूक़ी हाकिम (गवर्नर) अतसज़ ने सुल्तान संजर की मृत्यु के बाद डाली थी। ख़्वारिज़्म के बादशाहों अलाउद्दीन तकश (568 हि०/1172 ई० से 596 हि०/1200 ई०) और अलाउद्दीन मुहम्मद ख़्वारिज़्म शाह (596 हि०/1200 ई० से 617 हि०/1220 ई०) ने अपनी सल्तनत को बहुत बढ़ाया। अलाउद्दीन तकश ने ख़ुरासान फ़तह किया और अलाउद्दीन मुहम्मद ने एक ओर शहाबुद्दीन ग़ौरी की मृत्यु के बाद हरात और ग़ज़नी को ग़ौरियों से छीन लिया और दूसरी ओर मावराउन-नहर के इलाक़े से क़राख़िताइयों (क़रह ख़ताई) की हुकूमत का अन्त कर दिया। ये क़राख़िताई वही थे जिन्होंने सुल्तान संजर सलजूक़ी को पराजित कर मावराउन-नहर पर क़बज़ा कर लिया था। ख़्वारिज़्म शाह अब बग़दाद पर भी क़बज़ा करना चाहता था। ऐसा मालूम होता था कि इस्लामी दुनिया का बड़ा हिस्सा अब फिर संगठित हो जाएगा, परन्तु अल्लाह को यह मंज़ूर नहीं था।
इस्लामी दुनिया की उत्तर पूर्वी सीमा सैहून नदी के पश्चिम में बैकाल झील तक पहुँच गई थी। ख़तन, यारक़ंद, काशग़र और ताशक़ंद इस्लामी दुनिया के सीमावर्ती शहर थे। इन शहरों के बाद चीन तक एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जिसे गोबी रेगिस्तान कहते हैं। अफ़्रीक़ा के विशाल रेगिस्तान के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान से लगा हुआ एक देश है जो मंगोलिया कहलाता है।
मुहम्मद ख़्वारिज़्म शाह के ज़माने में मंगोलिया से चीन तक एक व्यक्ति चंगेज़ ख़ाँ (1206 ई० से 1227 ई०) ने एक विशाल हुकूमत क़ायम कर ली थी और चीन भी फ़तह कर लिया था। यह मंगोलों की हुकूमत थी जो मंगोलिया के रहनेवाले थे। ये मंगोल बड़े वहशी, उजड्ड और ख़ूँख़ार थे। चंगेज़ ख़ाँ अच्छे-अच्छे कपड़ों का शौक़ीन था और ये कपड़े चूँकि इस्लामी दुनिया में बनते थे इसलिए उसने एक बार कुछ व्यापारियों को ख़्वारिज़्म भेजा। मुहम्मद ख़्वारिज़्म शाह ने उन्हें जासूस समझकर क़त्ल करवा दिया। उसपर चंगेज़ ख़ाँ बहुत क्रोधित हुआ। बात थी भी ग़ुस्से की। व्यापारियों को बिना किसी क़ुसूर के क़त्ल कर देना कोई इनसाफ़ की बात नहीं। चंगेज़ ख़ाँ ने इसका कारण पूछा, परन्तु ख़्वारिज़्म शाह ने उसके संदेशवाहक को भी क़त्ल कर दिया। बस अब क्या था, चंगेज़ ख़ाँ वहशी मंगोलों की एक विशाल फ़ौज लेकर चढ़ आया और ख़्वारिज़्म शाह की सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार ख़्वारिज़्म शाह के कारण इस्लामी दुनिया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। ख़्वारिज़्म शाह ऐसा ज़ुल्म न करता तो वहशी मंगोल आक्रमण न करते। उसकी ज़रा-सी ग़लती से लाखों इनसानों को नुक़सान पहुँचा। परन्तु सबसे बुरी बात यह हुई कि ख़्वारिज़्म शाह ने चंगेज़ ख़ाँ से छेड़ तो शुरू कर दी, परन्तु जब उसने हमला किया तो एक जगह भी जंग के मैदान में आकर उसका मुक़ाबला नहीं किया। वह ऐसा भयभीत हुआ कि कहीं भी मुक़ाबला नहीं कर सका। चंगेज़ ख़ाँ शहर पर शहर फ़तह करता जाता और वह आगे-आगे भागता जाता था, यहाँ तक कि ख़िज़्र सागर के एक टापू आबसकोन में जाकर पनाह ली और वहीं 617 हि०/1220 ई० में इन्तिक़ाल किया।
मुहम्मद ख़्वारिज़्म के बाद उसके लड़के जलालुद्दीन ख़्वारिज़्म शाह ने जो बहुत वीर था, मुक़ाबला करने की कोशिश की। वह कई साल तक मंगोलों से लड़ता रहा, परन्तु कामयाब वह भी न हो सका।
मंगोलों का यह हमला बहुत बड़ी तबाही लाया। समरक़ंद, बुख़ारा, ख़्वारिज़्म, बल्ख़, नीशापुर, रै गोया इस्लामी दुनिया के वे सब शहर जो मध्य एशिया और ईरान में थे, उन्होंने बरबाद कर दिए। लोगों का क़त्ले आम किया। शहरों में आग लगा दी। शहरों की इमारतें जला दीं और देखते-देखते इस्लामी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा वीरान और जलकर राख हो गया। मस्जिदें, पुस्तकालय और मदरसे सब बरबाद कर दिए गए।
बुख़ारा और समरक़ंद जिनकी आबादी का अनुमान दस-दस लाख तक किया जाता है, बिलकुल तबाह कर दिए गए। समरक़ंद के साठ हज़ार कारीगरों को मंगोल बेगार में पकड़कर ले गए और शहर में केवल पाँच हज़ार आदमी ज़िन्दा बचे। ख़्वारिज़्म में क़त्ले आम के बाद मंगोलों ने जैहून नदी का बाँध तोड़ दिया जिस से पूरा शहर पानी में डूब गया। नीशापुर प्रांत में सत्रह लाख और हरात प्रांत में सोलह लाख आदमी क़त्ल किए गए। ये प्रांत जो इस्लामी सल्तनत में घनी आबादीवाले क्षेत्र थे, लगभग ग़ैर आबाद हो गए। शहर रै में सात लाख आदमी या तो क़त्ल कर दिए गए या क़ैदी बना लिए गए। मंगोलों की इस तबाही का उल्लेख एक समकालीन इतिहासकार ने चंद शब्दों में इस प्रकार किया है—
"वे आए, तोड़-फोड़ की, आग लगाई, लूटमार की और चले गए।"
इस काल के एक इतिहासकार इब्ने असीर जो चंगेज़ ख़ाँ के हमले के समय मौजूद थे, ने इन घटनाओं को विस्तार से लिखा है। उनके दिल पर इस्लामी तबाही का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। अतः वह लिखते हैं—
"यह हादसा इतना ख़ौफ़नाक और अप्रिय है कि मैं कई वर्ष तक इस दुविधा में रहा कि इसका उल्लेख करूँ या न करूँ। हक़ीक़त भी यह है कि इस्लाम और मुसलमानों की मौत की ख़बर सुनाना किसके लिए आसान है और किसका दिल है कि उनकी ज़िल्लत (अपमान) और रुसवाई की दास्तान सुनाए। काश! मैं पैदा न होता। काश! मैं इस घटना से पहले मर चुका होता। यह वह अज़ीम (बड़ा) हादसा है कि दुनिया के इतिहास में इसकी नज़ीर (उदाहरण) नहीं मिल सकती और शायद दुनिया क़ियामत तक भी ऐसी घटना न देखे।"
ख़्वारिज़्म शाह की सल्तनत और रै, हम्दान और आज़रबाइजान तक तमाम शहरों को तबाह करके चंगेज़ मंगोलिया वापस चला गया और कुछ समय बाद मर गया। परन्तु पचास वर्ष बाद उसके पोते हलाकू ख़ाँ ने एक क़दम और आगे बढ़ाया। उसने बग़दाद पर क़बज़ा करने का इरादा कर लिया, जो उस वक़्त इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था।
अब्बासी ख़िलाफ़त का अन्तिम काल
सलजूक़ियों के बाद बग़दाद के ख़लीफ़ा फिर संप्रभु हो गए थे। इन अन्तिम अब्बासी ख़लीफ़ाओं की सल्तनत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वे केवल इराक़ पर हुकूमत करते थे। बग़दाद, बसरा और कूफ़ा उनके क़बज़े में थे।
अन्तिम काल के ये अब्बासी ख़लीफ़ा जिनकी तादाद सात है, आख़िरी ख़लीफ़ा मुस्तअसिम के अतिरिक्त सब के सब योग्य और बुद्धिमान थे। उनमें मुक्तफ़ी का इसलिए महत्त्व है कि उसने सलजूक़ी आधिपत्य को समाप्त करने की सफल कोशिश की और 547 हि०/1152 ई० में सल्तनत को उनसे आज़ाद करा लिया।
नासिर की ख्याति इसलिए है कि उसने 47 साल हुकूमत की। अब्बासी ख़लीफ़ाओं में किसी ने इतनी लम्बी अवधि तक हुकूमत नहीं की। नासिर बहुत कठोर स्वभाव का था। उसने सल्तनत को बहुत मज़बूत कर दिया, परन्तु उसने लोगों पर टैक्स बहुत लगाए और धन प्राप्त करने के लिए लोगों पर बहुत कठोरता की। इसके साथ ही साथ उसने जनकल्याण के काम भी अंजाम दिए और मस्जिदें, ख़ानक़ाहें और मुसाफ़िरख़ाने बड़ी तादाद में बनवाए।
नासिर के बाद उसका लड़का ज़ाहिर गद्दी पर बैठा। वह अपने आचरण एवं व्यवहार में प्रथम चार ख़लीफ़ाओं का नमूना प्रतीत होता था। उसने अपने बाप के समय की कठोरता और ज़ुल्म को समाप्त कर दिया, परन्तु यह नेक ख़लीफ़ा केवल नौ महीने ख़िलाफ़त करके अपने ख़ुदा से जा मिला।
अन्तिम काल के अब्बासी ख़लीफ़ाओं में सबसे ज़्यादा नेक और प्रसिद्ध मुस्तंसिर है। वह अपने बाप ज़ाहिर के बाद ख़लीफ़ा हुआ। उसने कुल सत्रह साल हुकूमत की, परन्तु ये सत्रह साल अब्बासियों के अन्तिम काल का स्वर्णिम काल है। उसके काल में अत्यधिक मस्जिदें, ख़ानक़ाहें, मुसाफ़िरख़ाने, सराय और अस्पताल बनाए गए। उसने बग़दाद में एक ऐसा मदरसा बनवाया जिसके आगे निज़ामुल-मुल्क का मदरसा 'निज़ामिया' भी मांद पड़ गया। इस मदरसे का नाम ख़लीफ़ा के नाम पर मदरसा मुस्तंसिरिया था। इस मदरसे की इमारत सात साल में पूर्ण हुई। मदरसे का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसके लिए साठ ऊँटों पर किताबें लदकर आईं। जब यह मदरसा खुला तो इसमें ढाई सौ छात्रों ने प्रवेश लिया। छात्रों को मदरसे की ओर से खाने के अतिरिक्त मिठाइयाँ और मेवे भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त चटाइयाँ, फ़र्श, तेल, काग़ज़, दवात मुफ़्त मिलती थी और प्रत्येक छात्र को एक अशरफ़ी मासिक वज़ीफ़ा (छात्रवृत्ति) भी मिलता था। मदरसा में एक अस्पताल और एक अच्छा हम्माम भी था।
इस मदरसा की इमारत जीर्ण अवस्था में आज भी बग़दाद में मौजूद है। मुस्तंसिर ने जनकल्याण के इन कामों के अलावा सल्तनत को भी बहुत मज़बूत किया। उसका ज़माना बड़ा नाज़ुक था। चंगेज़ ख़ाँ की तातारी फ़ौजें ईरान और मावराउन-नहर को तबाह कर चुकी थीं और उसकी सल्तनत की सरहद अब्बासी ख़िलाफ़त से मिल गई थी। मुस्तंसिर ने इस ख़तरे की रोकथाम के लिए एक लाख सवार फ़ौज तैयार की। पयादा फ़ौज उसके अतिरिक्त थी।
बग़दाद के अन्तिम ख़लीफ़ा मुस्तअ्सिम बिल्लाह में हुकूमत चलाने की योग्यता नहीं थी। वह घमण्डी और मूर्ख था। उसने मुस्तंसिर की जमा की हुई फ़ौज भी तोड़ दी। उसने अपने मंत्री इब्ने अल्क़मी पर विश्वास किया, परन्तु उस मंत्री ने ग़द्दारी की और हलाकू को बग़दाद पर हमले के लिए बुला भेजा। हलाकू ख़ाँ ने चालीस दिन के घेराव के बाद बग़दाद को फ़तह कर लिया और मंगोल फ़ौजें बग़दाद में प्रवेश कर गईं। यह घटना सफ़र (अरबी कैलेण्डर का दूसरा महीना) 656 हि०/1285 ई० की है।

चित्र 7 :- बग़दाद का बाब अल-वस्तानी अब्बासी दौर की फ़सील शहर का वाहिद हिस्सा है जो अब तक महफ़ूज़ है। इस फ़सील की मरम्मत करने के बाद इस हिस्से को क़ौमी अजायबख़ाना में तबदील कर दिया गया है।

चित्र 8 :- अब्बासी दौर में बग़दाद अपने शानदार मदरसों की वजह से मशहूर था जो तातारियों के हमले के बाद बरबाद कर दिए गए। यह आसार मदरसा मुस्तन्सिरया के हैं जो ख़लीफ़ा मुस्तन्सिर बिल्लाह के हुक्म से 1232 ई० में तामीर हुआ था और ख़ुश क़िस्मती से उसका बड़ा हिस्सा अब तक महफ़ूज़ है।
बग़दाद हालाँकि उस ज़माने में उतना बड़ा शहर नहीं रहा था जितना अब्बासी ख़िलाफ़त के उत्थान के ज़माने में था, फिर भी वह दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ कई अस्पताल थे जिनमें सूक़-मारिस्तान का अस्पताल इतना बड़ा था कि उसमें बावन चिकित्सक नौकरी करते थे। दवा तैयार करनेवालों और मरीज़ों की देखभाल करनेवालों और दूसरे नौकरों की तादाद इसके अलावा थी।
हम्मामों की तादाद दो हज़ार थी। ये बड़े शानदार हम्माम होते थे। उनकी दीवारों और फ़र्श पर काले रंग की चमकदार पालिश थी। मस्जिदों की इतनी तादाद थी कि इब्ने जबीर ने लिखा है कि उनकी गिनती तो क्या अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। मस्जिदें बड़ी आलीशान थीं। बीस मदरसे थे और प्रत्येक मदरसे की इमारत ऐसी विशाल थी कि बड़े-बड़े महलों को शर्माती थी।
बग़दाद के पूर्वी भाग में आलीशान महल, मनमोहक बाग़ीचे और बड़े-बड़े बाज़ार थे। यह वह बग़दाद था जिसपर क़बज़ा करने के बाद वहशी तातारियों ने कई दिनों तक क़त्ले आम किया और चालीस दिन तक शहर को लूटते रहे। इमारतें ढा दीं, मकानों में आग लगा दी। मस्जिदें, मदरसे, अस्पताल जिनकी वजह से बग़दाद मशहूर था, बरबाद कर दिए गए और दुनिया का सबसे बड़ा शहर चंद दिनों में खंडहर बन गया। कहा जाता है कि बग़दाद में सोलह लाख मर्द-औरतों और बच्चों को मंगोलों ने क़त्ल किया।
मुस्तअ्सिम के साथ भी हलाकू ने बुरा सुलूक किया। उसे डंडों से पीट-पीटकर मार डाला और उसकी लाश को पैरों से मसलकर फेंक दिया।
इब्ने अलक़मी जिसने ग़द्दारी की थी उसके साथ तातारियों ने कोई सुलूक नहीं किया और चंद दिनों बाद वह भी मर गया।
इराक़ के दूसरे शहरों का भी यही हाल हुआ। इसके बाद हलाकू ने शाम (Syria ) का रुख़ किया और रूहा (Ruha), हर्रान और नसीबैन के वासियों का नरसंहार किया। फिर हलब में दाख़िल होकर पचास हज़ार लोगों को क़त्ल किया और दस हज़ार औरतों, बच्चों को ग़ुलाम बनाया। अन्ततः मिस्र के हुक्मरान बैबरस ने 15 रमज़ान, 658 हि०/1260 ई० को फ़िलस्तीन (Palestine) के एक स्थान पर ऐन जालूत में मंगोलों को पराजित कर शाम (Syria) एवं मिस्र (Egypt) को तबाह होने से बचा लिया। मावराउन-नहर से बग़दाद तक का इलाक़ा इस्लामी दुनिया का दिल था। मंगोलों के हमले से यह बिलकुल बरबाद हो गया। उन्होंने इराक़ की उन नहरों को भी बरबाद कर दिया जिससे इराक़ हरा-भरा रहता था।
मंगोलों के हमले को हालाँकि सात सौ वर्ष बीत चुके हैं और इस अवधि में यहाँ बड़ी-बड़ी हुकूमतें क़ायम हुईं, परन्तु इन मुल्कों में वह ख़ुशहाली, ज्ञान एवं कला का विकास फिर कभी नहीं देखा गया जो बग़दाद की तबाही के ज़माने तक इस क्षेत्र ने किया था। उस ज़माने में इस्लामी दुनिया का यह भूभाग ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और उद्योग-धंधे में सारी दुनिया से बढ़ा हुआ था। वर्त्तमान शताब्दी में आधुनिक विकास के बाद भी इस्लामी दुनिया को यह उच्च स्थान प्राप्त नहीं। मुसलमानों के इस पतन के विभिन्न कारण हैं, परन्तु एक बहुत बड़ा कारण मंगोलों का हमला और उनकी फैलाई हुई तबाही और बरबादी भी है। एक ओर अन्दलुस में इस्लामी सभ्यता और शहरों की तबाही और पुस्तकालयों एवं मदरसों की बरबादी ने और दूसरी ओर तुर्किस्तान से शाम (Syria) तक इस्लामी दुनिया की आत्मा की मंगोलों के हाथों तबाही ने इस्लामी दुनिया को पतन की ओर धकेल दिया। एक क़ौम के विकास में उसके बौद्धिक भंडारों, सांस्कृतिक संस्थाओं, उद्योग-धंधों और कृषि आदि की मुख्य भूमिका होती है। यदि ज्ञान एवं सभ्यता के ये चिह्न मलयामेट कर दिए जाएँ और शहर एवं बस्तियाँ वीरान कर दी जाएँ और सदियों की कोशिशों से जमा किया हुआ ज्ञान का भंडार बरबाद कर दिया जाए तो उस क़ौम की तबाही में, जो इन मुश्किलों का शिकार हो, क्या संदेह रह जाता है। यदि आज यूरोप और अमेरिका को भी ऐसी परिस्थिति से गुज़रना पड़े और उनके तमाम शहर खंडहर कर दिए जाएँ, उनमें हलचल मचा दी जाए, मदरसे, पुस्तकालय और ज्ञान-विज्ञान के खोज की संस्थाएँ समाप्त हो जाएँ और बड़े-बड़े शहरों के औरत, मर्द एवं बच्चों का क़त्ले आम कर दिया जाए तो शायद यूरोप का भविष्य भी इससे ज़्यादा भिन्न नहीं होगा, जो बग़दाद की तबाही के बाद इस्लामी दुनिया का हुआ। मंगोलों के हमले ने केवल भौतिक रूप से ही तबाही नहीं फैलाई, उसने अपनी वहशत और क्रूरता से मुसलमानों के हौसले भी पस्त कर दिए। उनके दिल तोड़ दिए जिसके परिणाम-स्वरूप निराशा का वातावरण और वैराग्य की इच्छा पैदा हो गई, और यह बात भी मुसलमानों के पतन का कारण बनी।
इब्ने जौज़ी
अब्बासी ख़िलाफ़त के इस अन्तिम काल में जो प्रसिद्ध लोग गुज़रे हैं उनमें हम अल्लामा इब्ने जौज़ी (508 हि०/1114 ई० से 597 हि०/1200 ई०) को कभी नहीं भूल सकते। इब्ने जौज़ी एक महान मुहद्दिस (हदीस-ज्ञाता), एक बड़े इतिहासकार और श्रेष्ठ सुधारक थे। वे बड़े साहसी थे और चाहते थे कि हर चीज़ में उसके चरम बिन्दु तक पहुँच जाएँ। वे अपनी किताब में अपनी इस इच्छा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं—
“मेरे अति उत्साही होने का मामला अजीब है, मैं इल्म का वह स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ तक मुझे यक़ीन है कि मैं पहुँच नहीं सकूँगा। मैं सभी तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ चाहे उसका विषय कुछ भी हो और प्रत्येक ज्ञान में उसकी पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर इल्म के साथ में अमल भी चाहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मुझमें बिश्र हाफ़ी की सावधानी और मारूफ़ करख़ी की धर्मपरायणता जमा हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि लोगों का मुहताज न रहूँ, लोगों का एहसान लेने के बदले उनपर एहसान करने के योग्य हो सकूँ। मुझे औलाद की भी इच्छा है और उत्कृष्ट कोटि की पुस्तक रचने का भी शौक़ है। मुझे अच्छी चीज़ों से जायज़ लुत्फ़ लेने का शौक़ है, उसी प्रकार मैं ऐसे आहार एवं खाने-पीने की चीज़ों का शौक़ीन हूँ, जो शरीर के लिए लाभदायक हों। फिर मेरी यह भी इच्छा है कि दुनिया को इस प्रकार प्राप्त करूँ कि मेरे दीन पर आँच न आए। मेरी बेचैनी का कोई क्या अन्दाज़ा कर सकता है, एक ओर मुझे रातों को जागकर इबादत करने एवं अपने ईश-भय पैदा करने की चिन्ता है और दूसरी ओर ज्ञान का प्रचार, लेखन और शरीर के लिए समुचित आहार की भी आवश्यकता है। एक ओर लोगों से मिलना-जुलना और उनकी शिक्षा भी ज़रूरी है, दूसरी ओर तन्हाई में इबादत एवं दुआ के लुत्फ़ में कमी हो तो उसपर भी अफ़सोस होता है। घरवालों के लिए जीवन यापन की वस्तुओं की व्यवस्था की जाए तो इबादत के स्तर में अन्तर आता है। परन्तु मैंने सारे कष्टों एवं असुविधाओं को अपना रखा है। शायद मेरा सुधार और विकास इसी कष्ट एवं संघर्ष में है। इसलिए कि बुलंद हिम्मतवाले लोग ऐसे कर्मों की चिन्ता में रहते हैं जो ख़ुदा के यहाँ सम्मान एवं निकटता के कारण हैं। यदि मेरा उद्देश्य प्राप्त हो गया तो सुब्हानल्लाह, वरना एक मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है।"
यह वह ज़माना था जब मुसलमानों में माल एवं दौलत की अधिकता और सभ्यता एवं संस्कृति की सुविधाओं के कारण बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो गई थीं और उनके अख़लाक़ बिगड़ गए थे। लोगों की यह हालत देखकर इब्ने जौज़ी का दिल बहुत दुखी होता था और अन्ततः उन्होंने भी लोगों के सुधार के लिए वही तरीक़ा अपनाया जो उनसे कुछ ही पहले ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) और अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) अपना चुके थे। इब्ने जौज़ी ने सुधार के लिए किताबें भी लिखीं और उपदेश एवं भाषण भी दिए। उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह), अहमद बिन हंबल और बड़े-बड़े लोगों के हालात भी लिखे जिनकी ज़िन्दगी इस्लामी जीवन चरित्र का नमूना थीं। इससे इब्ने जौज़ी का मक़सद यह था कि लोग उन महान हस्तियों के हालात पढ़कर अपनी ज़िन्दगी भी वैसी ही बनाने का प्रयास करें।
इब्ने जौज़ी एक उच्च कोटि के वक्ता भी थे। उनके सुधारात्मक भाषणों से सारे बग़दाद में हलचल मच गई थी। उनके इन भाषणों और दर्स की मजलिसों में एक-एक लाख आदमी जमा हो जाते थे। अनुमान लगाया गया है कि एक लाख आदमियों ने उनके हाथ पर बुरे कामों से तौबा की और बीस हज़ार यहूदियों और ईसाइयों ने उनके हाथ पर इस्लाम क़बूल किया। यह उनका इतना बड़ा कारनामा है जिसकी मिसाल शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) के अलावा इतिहास में शायद ही किसी दूसरी जगह मिले।
इब्ने असीर और याक़ूत हमवी
अब्बासियों के अन्तिम काल में इब्ने जौज़ी के अलावा भी कई महान लेखक हुए हैं। उनमें एक इब्ने असीर (555 हि०/1160 ई० से630 हि०/1234 ई०) हैं। वे 'तारीख़ अल-कामिल' नामक एक किताब के लेखक हैं जिसमें इस्लाम के प्रारंभ से 1230 ई० तक का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यह किताब इस्लामी इतिहास की प्रमुख किताबों में गिनी जाती है। इब्ने असीर की दूसरी प्रमुख किताब 'तारीख़ अताबक-ए-मोसल' है। यह ज़ंगी ख़ानदान का सबसे प्रमाणिक और विस्तृत इतिहास है। इब्ने असीर की तीसरी बड़ी किताब 'असदुल-ग़ाबा' है जिसमें कई सौ सहाबा की जीवनियाँ लिखी गई हैं।
इस काल के एक और महान व्यक्ति याक़ूत हमवी (575 हि०/1179 ई० से 626 हि०/1229 ई०) हैं। हमवी अपने दौर के सबसे बड़े भूगोलविद् और पर्यटक थे। भूगोल में उनकी किताब 'मुअजमुल-बुल्दान' बहुत उच्च कोटि की समझी जाती है। इसके अलावा याक़ूत 'मुअजमुल-उदबा' नामक एक और किताब के लेखक भी हैं जिसमें कई सौ अदीबों (साहित्यकारों), लेखकों और शायरों के हालात लिखे हैं।
ख़्वारिज़्म शाही सल्तनत
(551 हि०/1156 ई० से 628 हि०/1231 ई०)
1. अरसलान - 551 हि०/1156 ई० से 566 हि०/1170 ई०
2. सुल्तान शाह - 566 हि०/1170 ई० से 568 हि०/1172 ई०
3. अलाउद्दीन तकश - 568 हि०/1172 ई० से 596 हि०/1200 ई०
4. अलाउद्दीन मुहम्मद - 596 हि०/1200 ई० से 617 हि०/1220 ई०
5. जलालुद्दीन - 617 हि०/1220 ई० से 628 हि०/1231 ई०
बग़दाद के अन्तिम ख़लीफ़ा
(547 हि०/1152 ई० से 656 हि०/1258 ई०)
1. मुकतफ़ी-बिअमरिल्लाह - 530 हि०/1136 ई० से 555 हि०/1160 ई० सलज़ूकी हुकूमत से
547 हि०/1152 ई० में आज़ादी हासिल कर ली।
2. मुस्तंजिद बिल्लाह - 555 हि०/1160 ई० से 566 हि०/1170 ई०
3. मुस्तज़ी बि-अमरिल्लाह - 566 हि०/1170 ई० से 575 हि०/1180 ई०
4. अन-नासिरुद्दीन - 575 हि०/1180 ई० से 622 हि०/1225 ई०
5. ज़ाहिर बि-अमरिल्लाह - 622 हि०/1225 ई० से 623 हि०/1226 ई०
6. मुस्तंसिर बिल्लाह - 623 हि०/1226 ई० से 640 हि०/1242 ई०
7. मुस्तअ्सिम बिल्लाह - 640 हि०/1242 ई० से 656 हि०/1258 ई०
★ 615 हि०/1218 ई० - ख़्वारिज़्म शाही सल्तनत पर चंगेज़ ख़ाँ के हमले का प्रारम्भ
★ 617 हि०/1220 ई० - बुख़ारा, समरक़ंद और ख़्वारिज़्म पर क़बजा
★ 618 हि०/1221 ई० - नीशापुर और उसके बाद रै एवं हमदान की तबाही
★ 619 हि०/1222 ई० - चंगेज़ ख़ाँ की मंगोलिया वापसी
अध्याय-23
मुसलमानों के उत्थान के प्रथम दौर का अन्त
तातारियों के हाथों बग़दाद की तबाही और अन्दलुस (Andalus) में मुसलमानों के पतन के बाद इस्लामी इतिहास का एक प्रमुख दौर समाप्त हो जाता है। यह दौर मुसलमानों के उत्थान का पहला दौर है। इसका प्रारंभ 1 हिजरी/622 ई० में मदीना में इस्लामी हुकूमत के स्थापित होने से होता है और 656 हि०/1258 ई० में बग़दाद की तबाही पर इस प्रथम दौर का अन्त हो जाता है। बग़दाद हालाँकि तबाह हो गया, इस्लामी दुनिया का बड़ा हिस्सा तातारियों के क़बज़े में चला गया और अन्दलुस मुसलमानों के हाथ से निकल गया, परन्तु जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा, इन तमाम नुक़सानों और तबाहियों के बावजूद मुसलमानों का पतन अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। बग़दाद की तबाही के बाद भी पूरे साढ़े चार सौ साल तक मुसलमानों का उत्थान रहा। साढ़े चार सौ साल का यह ज़माना मुसलमानों के उत्थान का दूसरा दौर है। यहाँ यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों के उत्थान के पहले दौर की क्या विशेषताएँ हैं, ताकि बाद में उत्थान के प्रथम दौर और द्वितीय दौर का अन्तर अच्छी तरह समझा जा सके। प्रथम दौर की विशेषताएँ निम्न हैं :-
1. इस्लामी सल्तनत क्षेत्रफल के लिहाज़ से दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत बन गई थी। अरबों के उत्थान काल में जबकि दमिश्क़ और बग़दाद इस्लामी सल्तनत की राजधानियाँ थीं, इस्लामी सल्तनत जितनी विशाल सल्तनत उस वक़्त तक दुनिया में किसी क़ौम ने क़ायम नहीं की थी। ईरान की कियानी सल्तनत, अतालिया की रूमी सल्तनत और चीन की तांग सल्तनत जो प्राचीन काल में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमतें थीं, क्षेत्रफल में इस्लामी हुकूमत से बहुत कम थीं।
2. उस दौर में मुसलमान केवल सियासी तौर पर ही उत्थान के चरम पर नहीं पहुँचे, बल्कि बौद्धिक लिहाज़ से भी चरमोत्कर्ष पर पहुँचे। अतः उस ज़माने में मुसलमानों में जैसे बड़े-बड़े लेखक हुए और उन्होंने तफ़सीर, हदीस, दर्शन, गणित, चिकित्सा, इतिहास और भूगोल आदि पर जैसी अच्छी किताबें लिखीं और जैसे आविष्कार किए वैसा उस दौर में दुनिया में किसी क़ौम ने नहीं किया। उस दौर की रचनाएँ सृजनात्मक थीं। यानी उनमें एक नई बात और नई कल्पना प्रस्तुत की जाती थी। यही कारण है कि ये किताबें क्लासिकी समझी जाती हैं। ये किताबें बाद में लिखी जानेवाली किताबों के लिए एक प्रकार की बुनियाद (स्रोत) बन गईं।
3. इस दौर में अरबी तमाम मुसलमानों की वैज्ञानिक भाषा थी। तुर्क, ईरानी, हबशी, बर्बर तमाम क़ौमों के विद्वान लेखन कार्य हेतु अरबी भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। अरबी ज़बान तमाम मुसलमानों की संयुक्त ज़बान थी जिसके कारण मावराउन-नहर में लिखी हुई किताबें अन्दलुस तक और अन्दलुस में लिखी किताबें मावराउन-नहर तक आसानी से फैल जाती थीं। इसके कारण पूरी इस्लामी दुनिया के मुसलमान एक-दूसरे के विचारों से अवगत रहते थे। बाद में जब इस्लामी दुनिया में फूट पैदा हो गई और एक की जगह कई-कई हुकूमतें क़ायम हो गईं तो यही अरबी ज़बान थी, जिसके ज़रिये मुसलमानों में एकता बनी हुई थी। अरबी उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा बन गई थी।
एक पश्चिमी शोधकर्ता जार्ज सार्टन ने सम्पूर्ण दुनिया का एक बौद्धिक इतिहास संकलित किया है। इसमें उसने इस्लामी इतिहास के उस दौर के सम्बन्ध में लिखा है :-
“मध्य काल में सबसे अधिक महान कारनामे मुसलमानों ने अंजाम दिए। यह सही है कि उस ज़माने में लातीनी ज़बान में भी कई प्रमुख किताबें लिखी गईं। उसी प्रकार यूनानी, सिरयानी, फ़ारसी, संस्कृत और चीनी यहाँ तक कि जापानी ज़बान में भी कुछ प्रमुख किताबें लिखी गईं परन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, सबसे अधिक सामर्थ्य रखनेवाली और सबसे अधिक परिणामदायक एवं लाभदायक किताबें अरबी में लिखी गईं। आठवीं सदी के उत्तरार्द्ध से ग्यारहवीं सदी तक अरबी मानव जाति की प्रगतिशील ज़बान थी। उस ज़माने में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर प्रकार का और आधुनिकतम ज्ञान अर्जित करना चाहता हो अरबी ही पढ़नी पड़ती थी। अतः वे लोग जो ग़ैर अरब थे, उन्होंने अधिकतर ऐसा ही किया। बिलकुल उसी प्रकार जिस प्रकार इस ज़माने में एक ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक विकास करना चाहता हो तो उसके लिए बड़ी-बड़ी पश्चिमी ज़बानों में से किसी एक ज़बान का सीखना अनिवार्य है।"
4. उस दौर में मुसलमान इस्लामी शिक्षाओं से बहुत निकट थे। ख़िलाफ़ते राशिदा का ज़माना भी उसी दौर में आता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, निज़ामुल-मुल्क तूसी, नूरुद्दीन, सलाहुद्दीन, हिशाम प्रथम, अब्दुल मोमिन और अबू याक़ूब अल-मंसूर जैसे अच्छे हुक्मरान इस दौर में हुए। इन हुक्मरानों ने अपने ज़माने में इस्लामी उसूलों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश की। इसके अलावा इमाम अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह), इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह), इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह), इमाम अहमद बिन हंबल (रहमतुल्लाह अलैह), इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह), इब्ने हज़्म और अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहमतुल्लाह अलैह) जैसे आलिम इसी दौर में हुए। इनकी कोशिशों के कारण मुसलमानों में ज़्यादा ख़राबियाँ नहीं फैल सकीं और मुसलमान ग़ैर इस्लामी प्रभाव से बचे रहे, उनकी अख़लाक़ी हालत अच्छी रही।
5. सांस्कृतिक रूप से इस्लामी दुनिया सारी दुनिया से आगे बढ़ गई। यहाँ बग़दाद, कूफ़ा, समरक़ंद, बुख़ारा, रै, क़ाहिरा, मराकश, फ़ास, क़ुरतुबा, इशबीलिया जैसे विशाल शहरों की बहुलता थी और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इन शहरों में प्रत्येक की कई-कई लाख आबादी थी। इनकी सड़कें पक्की होती थीं। सफ़ाई-सुथराई का ख़याल रखा जाता था। इमारतें पक्की और कई-कई मंज़िलों की होती थीं। शहरवालों के लिए कई बग़ीचे और मनोरंजन स्थल होते थे।
प्रत्येक शहर में हम्माम, मस्जिदें, अस्पताल और मदरसे होते थे। लोगों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय होते थे और लोग निजी पुस्तकालय भी रखते थे। खगोलशास्त्र के लिए जगह-जगह ऐसी व्यवस्था होती थी जहाँ से सितारों का अध्ययन किया जा सके।
इन शहरों में अच्छे क़िस्म का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा तैयार होता था। अच्छे क़िस्म के चमड़े का सामान बनता था। इत्र बनाए जाते थे। तलवारें और हथियार बनते थे। पानी के जहाज़ बनते थे। खगोलशास्त्र और चिकित्सा में इस्तेमाल होनेवाले यंत्र बनाए जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर शहर हर क़िस्म के उद्योग-धंधे का केन्द्र था।
उस ज़माने में इस्लामी दुनिया और यूरोप में जो अन्तर था उसका अनुमान निम्न सूची से लगाया जा सकता है।
इस्लामी दुनिया और यूरोप में अंतर
(750 ई० और 1258 ई० के बीच)
इस्लामी दुनिया
1. दो दर्जन से अधिक शहर ऐसे थे जिनकी आबादी एक लाख से अधिक थी। बसरा, कूफ़ा और इशबीलिया की आबादी पाँच-पाँच लाख, क़ाहिरा दस लाख, क़ुरतुबा की पंद्रह लाख और बग़दाद की आबादी 265 लाख थी।
2. हर शहर में पक्की इमारतें होती थीं। बड़े शहरों में पाँच से आठ मंज़िल तक की इमारतें थीं और बड़े मकानों के साथ लॉन होते थे।
3. शाहरों में पक्की सड़कें होती थीं। गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी-बड़ी नालियाँ होती थीं।
4. शिक्षा का आम प्रचलन था और शिक्षा निःशुल्क थी। बड़े मदरसों में छः हज़ार तक छात्र होते थे।
5. प्रत्येक शहर में पुस्तकालयों की बहुतात थी। आम पुस्तकालय भी होते थे और निजी भी।
6. आम तौर पर बड़े शहरों में खगोलशास्त्र के अन्वेषण के लिए अध्ययन-केन्द्र होता था।
7. हर देश में काग़ज़ बनाया जाता था।
8. शीशा-निर्माण की कला पूरे उत्थान पर थी।
9. अच्छे क़िस्म का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा तैयार होता था।
10. बर्फ़ बनाने का उद्योग मौजूद था।
11. इलाज के लिए जगह-जगह आलीशान अस्पताल थे।
12. प्रत्येक शहर में बहुलता से हम्माम होते थे।
यूरोप
1. सिवाय क़ुस्तनतीनिया (Qustantiniyah) के एक शहर भी ऐसा नहीं था जिसकी आबादी एक लाख हो। रूम और फ़्लोरेन्स सबसे बड़े शहर थे जिनकी आबादी क्रमशः पचास हज़ार और पैंतालिस हज़ार थी। लंदन की 25 हज़ार थी। बारहवीं सदी में पूरे इंग्लैण्ड की आबादी केवल 22 लाख थी।
2. यूरोप के तमाम शहरों में मकान अधिकतर कच्ची मिट्टी के या घास-फूस और लकड़ी के होते थे।
3. शहरों की सड़कें अधिकतर कच्ची होती थीं। गंदे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण सड़कों और रास्तों पर कीचड़ रहती थी।
4. मदरसों का नाम नहीं था, सिवाय पादरियों के और कोई पढ़ना-लिखना नहीं जानता था। बारहवीं सदी ई० से मदरसे क़ायम होना शुरू हुए।
5. एक भी उल्लेखनीय पुस्तकालय नहीं था।
6. खगोलशास्त्र के अन्वेषण के लिए कोई अध्ययन केन्द्र नहीं था।
7. काग़ज़ बनाना नहीं जानते थे।
8. शीशा-निर्माण से अनभिज्ञ थे।
9. भद्दे क़िस्म के कपड़े तैयार होते थे। बड़े लोगों के घरों में इस्लामी मुल्कों के कपड़ों की माँग रहती थी।
10. यूरोपवालों ने सोलहवीं सदी में बर्फ़ बनाना सीखा।
11. दवा-इलाज से अनभिज्ञ थे। टोना-टोटकों से इलाज करते थे। पहला अस्पताल तेरहवीं सदी में रूम में बना।
12. हम्माम बनाना पाप का काम समझा जाता था।
यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्लामी दुनिया को ज्ञान एवं कला और सभ्यता एवं संस्कृति में यह अनुपम श्रेष्ठता केवल यूरोप के देशों के मुक़ाबले में प्राप्त नहीं थी, बल्कि पूरब के देशों और विशेषकर भारत एवं चीन के मुक़ाबले में भी इस्लामी दुनिया को सर्वोच्चता प्राप्त थी।
उस ज़माने में भारत और चीन में भी बड़े-बड़े शहर थे। बड़ी अच्छी हुकूमतें क़ायम थीं। बेहतरीन इमारतें बनाई जाती थीं। नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी। उद्योग एवं कृषि विकासोन्मुख थी। सूती कपड़ों में भारत और रेशमी कपड़ों में चीन इस्लामी दुनिया के देशों से किसी प्रकार पीछे नहीं थे। शून्य का प्रयोग एवं अंकों का ज्ञान मुसलमानों ने हिन्दुओं से सीखा। इसी प्रकार काग़ज़ बनाना और क़ुत्बनुमा (दिशा सूचक यंत्र) का प्रयोग मुसलमानों ने चीन के लोगों से सीखा, परन्तु इसके बावजूद हम यही कहेंगे कि इस्लामी दुनिया उस ज़माने में कुल मिलाकर भारत और चीन से भी आगे बढ़ गई थी।
भारत में बड़े-बड़े शहर ज़रूर थे, परन्तु ये शहर उतने सुन्दर और योजनानुसार नहीं होते थे जितने इस्लामी दुनिया के शहर थे। मनोरंजन स्थलों, बाग़ों और फ़व्वारों का तो भारत में रिवाज ही नहीं था। न यहाँ के शहरों में ऐसे अस्पताल थे जैसे मराकश, क़ाहिरा, दमिश्क़ आदि में थे और जिनका हाल हम पढ़ चुके हैं। न यहाँ इस्लामी शहरों की तरह शानदार मदरसे (स्कूल) थे और न यहाँ के लोग काग़ज़ बनाना जानते थे। फिर भारतवाले भूगोल और इतिहास से भी अनभिज्ञ थे। इन विषयों में उनकी अनभिज्ञता का यह हाल था कि वे स्वयं अपना इतिहास और अपने देश तक से अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं थे। अगर अल-बैरूनी, इब्ने हौक़ल और दूसरे मुसलमान इतिहासकार भारत के हालात न लिखते तो आज हम न तो यहाँ के बहुत-से शहरों के हालात जान पाते और न यहाँ के इतिहास की ही जानकारी हो पाती।
भारत के हिन्दू नागरिक तो बस अपने देश में ही रहते थे। समुद्र के उस पार जाना पाप समझते थे। जब ऐसा था तो भला यहाँ मसऊदी, इब्ने हौक़ल और इब्ने ज़ुबैर जैसे पर्यटक कैसे पैदा हो सकते थे।
भारत में एक और ख़राबी थी कि यहाँ जात-पात का भेदभाव था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। मुसलमानों में यह बात नहीं थी। इनके यहाँ ग़ुलाम भी बादशाह बन जाते थे और मामूली से मामूली काम करनेवाले मज़दूर और कारीगर भी बड़े-बड़े आलिम हो सकते थे।
चीन का हाल तो काफ़ी बेहतर था। मुसलमान वहाँ के लोगों से भी बहुत-सी बातों में आगे थे। चीनवाले एक ज़माने में बहुत अधिक परिभ्रमण करते थे, परन्तु जब से मुसलमानों का उत्थान हुआ तो उनका भी सैर-सपाटा व परिभ्रमण समाप्त हो गया। फिर ज्ञान प्राप्त करने के मामले में वे चीन ही के अन्दर बंद रहते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि वे चिकित्साशास्त्र, खगोलशास्त्र, विज्ञान एवं भूगोल में मुसलमानों की तरह प्रगति नहीं कर सके और इन विषयों में पाँच सौ साल की अवधि में शायद दो-चार लेखक भी ऐसे नहीं हुए जो मुसलमान विद्वानों के मुक़ाबले में पेश किए जा सकें।
चीनवाले अधिक से अधिक ईरान तक के हालात से वाक़िफ़ थे, परन्तु मुसलमान चीन से लेकर अटलांटिक महासागर के तट तक बल्कि अफ़्रीक़ा के विशाल रेगिस्तान के उस पार तक के देशों के हालात से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। चीनवाले इन इलाक़ों के नाम से भी वाक़िफ़ नहीं थे।
मुसलमानों ने एक ओर चीन से काग़ज़ निर्माण और क़ुत्बनुमा (दिशा सूचक यंत्र) का प्रयोग सीखा और दूसरी ओर यूरोपवालों को सिखाया।
मुसलमानों ने एक ओर भारत से अंको का ज्ञान सीखा और दूसरी ओर यूरोपवालों को सिखाया। उन्होंने भारत और चीन के चिकित्सा विधि को मिलाकर एक नई चिकित्सा पद्धति बनाई और भारत में होनेवाले फल और फूलों की इस्लामी देशों में खेती की और उनका ज्ञान यूरोप तक पहुँचा दिया।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 150 हि०/767 ई० से 650 हि०/1252 ई० तक के ज़माने में जो पाँच सौ साल [आठवीं (ई०) शताब्दी के मध्य से तेरहवीं (ई०) शताब्दी के मध्य तक] की अवधि है, दुनिया में सबसे अधिक सभ्य, विकसित, सुसंस्कृत और ज्ञान एवं कला का केन्द्र इस्लामी दुनिया के देश थे। मुसलमानों के बाद सभ्यता एवं संस्कृति में भारत और चीन आगे थे और सबसे पिछड़े, अल्पविकसित, असभ्य और जाहिल वे देश थे जो ईसाई-यूरोप में आते थे। यही कारण है कि यूरोप के इतिहास में मध्यकाल का ज़माना 'अंधकाल' (Dark Age) कहलाता है। परन्तु यूरोप के बहुत-से इतिहासकार एवं लेखक जिनकी किताबें हमारे यहाँ बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं, अपनी अज्ञानता के कारण पूरे विश्व के मध्यकाल को 'अंधकाल' कह डालते हैं। इस्लामी इतिहास के विद्यार्थी को कभी यह धोखा नहीं हो सकता। वह जब मध्यकाल का शब्द पढ़ता है तो उसके दिमाग़ में विचार आता है कि वह हमारा 'स्वर्णिम युग' था। इस्लामी दुनिया का पतन कैसे प्रारम्भ हुआ और यूरोप अपने 'अंधयुग' से किस प्रकार निकला और उसने वर्तमान तरक़्क़ी किस प्रकार प्राप्त की, इसका उल्लेख इस पुस्तक के दूसरे खण्ड में किया गया है।
ऐतिहासिक व्यक्तियों, स्थलों और परिभाषाओं के नाम
Abencuzman, Ibn Quzman इब्ने क़ुज़मान
Abyssinia हबश
Adana अज़ाना, अतना, अदाना
Adata अल-हदस
Adriatic आदरयास
Aghlabids अग़ालिबा
Alarcos अल-अरक
Albacete अल-बसीत
Albarracin बनवाज़ीन
Albategnius, Al-Bustani अल-बुस्तानी
Alcazar अल-क़सर (इशबीलिया)
Algecira अल-जज़ीरा (अन्दलुस)
Aleppo हलब
Alexandretta अस्कंदरूना
Alexandria अस्कंदरिया
Alfraganus अल-फ़रग़ानी
Algarve अल-ग़रब (अन्दलुस)
Al-Gazzali, Algazel अल-ग़ज़ाली
Algeciras जज़ीरा अल-ख़िज़रा (अन्दलुस)
Algiers अल-जज़ायर
Alhazen इब्ने हैसुम
Al-Mousil (Mosul) अल-मौसिल, मोसल
Aljarafe अस-सर्फ़ (अन्दलुस)
Almagest अल-मजिस्ती
Almeria अल-मेरिया, मारिया
Almadovar de Rio हिस्नुल मदूर
Almohades मुवह्हिदीन
Almoravids अल-मुराबतीन
Al-Mousil (Mousal) अल-मौसिल, मोसल
Almunecar अल-मुनक्कब (अन्दलुस)
Alpetragius अल-बतरूजी
Alpharabius अल-फ़ाराबी
Alpuente अल-बूनत
Alpuxarras (Alpujarras) अल-बुशारात
Amida आमद, दयारे बकर
Amorium अम्मूरिया
Amysos सामसून (तुर्की)
Antiocn अंताकिया
Apologos उबल्ला
Arabian Nights अल्फ़ लैला
Aragon अरग़ुन (अन्दलुस)
Araxes अरस (नदी)
Archimedes अर-ख़मीदिस, अर-शमीदस
Aristotle अरस्तू
Arsamosota ख़रबूत, शमशात
Arzachel अज़-ज़रक़ाली
Astorga अशतूरक़ा, अस्तूरगा
Asturias अस्तूरयास
Athens एथेंस, अतीना
Avempace इब्ने बाज्जा
Avendeath इब्ने दाऊद
Avenzoar इब्ने ज़ुहर
Averros इब्ने रुश्द
Avica जज़ीरा याबसा
Avicebron इब्ने जिबरील
Avicenna इब्ने सीना
Avignon अवीनून (फ़्रांस)
Bahrain, Behrain बहरैन
Babylonia बाबिल
Babylon बाबलियोन
Byzantion बोज़नतिया, क़ुस्ततीनिया का प्राचिन नाम, इस्तम्बूल
Badajoz बतल्यूस
Baeza बैज़ा, बैयासा
Barcelona बारसिलोना, बरशलोना
Beja बाजा (अन्दलुस)
Biscay बिशकंस (ख़लीज)
Bone बूना (अल-जज़ाइर)
Bordeaux बरजील, बोरदू
Bougie बजाया
Burgos बरग़ुश
Cadiz क़ादिस (अन्दलुस)
Caesarea क़ैसरिया, क़ैरी
Cairo क़ाहिरा
Calabria क़लयूबिया (इटली)
Calatayud क़िला अय्यूब
Calatrava क़िला रबाह
Calatrava la Veija कलतरावा ला विज़ा
Cambay कैम्बे, खंबाईत
Canamusali अम्मार मूसली
Canaries जज़ाइर सआदत
Canton ख़नफ़ू
Carcassonne क़रक़शूना (फ़्रांस)
Carmatniane क़रामिता
Carmona क़रमूना
Casablanca कासा बलंका, दारुल बैज़ा (मराकश)
Caspian कैस्पीयन, जरजान, तबरिस्तान (सागर)
Castamon क़स्तमून, क़स्तमूनिया
Castellon क़श्तिलून
Castile क़श्ताला, क़श्तालिया
Catalonia क़ैतलूनिया
Ceuta सब्ता (मराकश)
Ceylon श्रीलंका, सरांदीप
Chaboras ख़ाबूर नदी
Chosroes ख़ुसरव, ख़ुसरू
Cintra शिन्तरा, सिन्तरा
Circeium क़रक़ीसिया
Cilicia कलीकिया
Claudiopolis बोलो, बोली (तुर्की)
Claudias क़ुलौज़िया
Clsama क़ुलज़ुम, क़ुलज़म
Constantine क़ुस्तन्तीन
Constantine son of Luke क़ुस्ता बिन लूक़ा
Coustantinople क़ुस्तनतीनिया
Cordova क़ुरतुबा
Crete अक़रीतश, क्रेट
Ctesiphon तीसीनून, मदाइन
Cuenca कोनका (अन्दलुस)
Cyprus क़बरस
Cyrenica बरक़ा
Damascus दमिश्क़
Damietta दिमयात (मिस्र)
Darro हदारा नदी (अन्दलुस)
Denia दानिया (अन्दलुस)
Dome of Rock क़ुब्बतुस-सख़रा
Dorylean दरूलिया
Douro दवीरो, दौरो (नदी)
Ebro एबरो नदी (अन्दलुस)
Ecbastana हमदान
Edessa, Ar-Ruha, Urfa अर्रुहा, उरफ़ा, (तुर्की)
Edrisi इदरीसी
Egypt मिस्र
Elvira अलबीरा
Ephesos अफ़सुस (तुर्की)
Escorial एसकोरियल
Ethopia नहबशा
Etna जबलुल-बुरकान, एटना (पहाड़)
Euclid अक़लीदस
Euphrates फ़ुरात नदी
Fargana, Farganakeya Obast फ़रग़ाना
Farragat फ़रह बिन सालिम
Fes, Fez, Fas फ़ेस, फ़ेज़, फ़ॉस
Galen जालीनूस
Galicia जलीक़िया (अन्दलुस)
Garcia ग़रसिया (हुक्मरान)
Geber जाबिर इब्ने हय्यान
Generalife जन्नतुल-आरिफ़
Gerona जिरूना, जरन्दा
Gibralter जबलुत्-तारिक़, जिबराल्टर
Goths क़ौमे लूत
Granada ग़रनाता
Greece, Rûm रूम
Guadelete वादी लका, वादी लता (अन्दलुस)
Guadiana वादी आना (अन्दलुस)
Guadalaviar वादी अबयज़
Guadix वादी आश (अन्दलुस)
Guadalajara वादी हिजारा (अन्दलुस)
Guadalquivir वादी अल-कबीर (अन्दलुस)
Haly Rodoam अली इब्ने रिज़वान
Halys आलीस, क़ज़ल ईरमाक़ (तुर्की)
Hangchou ख़ंसा, ख़िंसा (चीन)
Heraclia हिर्क़ला (तुर्की)
Heraclius हिरक़्ल, हिराक्लयूस
Hierapolis मंबिज (सीरिया)
Hippocrates बुक़रात
Hittin हित्तीन
Homs, Hims हिम्स
Huesca वश्क़ा
Inconium क़ौलिया
Isfahân इस्फ़हान
Istambûl इस्तंबूल
Jaen जय्यान
Jativa शातिबा
Jaxartes सीर, सीहून (नदी)
Jerusalem यरूशलम, बैतुल-मक़्दिस
Jesualy अली इब्ने ईसा
Kamacha कमख़ (तुर्की)
Karauan क़ैरवान
Karallia बैशहर, बकशहरी (तुर्की)
Khanfu कैंटन (चीन)
Khazar ख़जर
Kinanah किनाना
Kinsa ख़ंसा, (हाँग चाऊ)
Kiphas (Cephe) हिस्न कैफ़ा (तुर्की)
Larache अल-अराइश (मराकश)
Lebnon, Lubnan लुबनान
Larida लारदा
Lisbona लशबूना
Loadicia लाज़क़्क़िया (तुर्की)
Lombardy लम्बारदी
Lorca लूरक़ा
Lyons हिस्न लौज़ून
Lugo लक
Luxor अक़सर
Madrid मजरीत
Magazin मख़ाज़िन
Magnesia मग़नीसा, मनीसा
Maimonides, Moses मूसा इब्ने मैमून
Majorea मयूरक़ा (टापू)
Marasion मरअश (तुर्की)
Malaga मालक़ा
Martyropolis मैयाफ़ारक़ीन (तुर्की)
Media अल-जिबाल (ईरान)
Medinaceli मदीनतुस-सालिम (अन्दलुस)
Massawa मसव्वा
Melitene मल्लातिया
Merida मारिदा (अन्दलुस)
Merv, Marw मर्व
Messina मस्सीना
Minorca मनोरक़ा (द्वीप)
Mesopotamia इराक़
Moracco मराकश
Moriscos मुवल्लदीन
Mozaribe मुस्तारिब
Murcia मुरसिया
Narbonne नरबूना, अरबूना (अन्दलुस)
Navarra नबरा (अन्दलुस)
Neo-Caesarea निकसार
Nazareth नासिरा (फ़लस्तीन)
Nicaea इज़नीक़
Nicephoros नक़फ़ूर (क़ैसरे रूम)
Nicomedia नज़ीब (तुर्की)
Nicopolis निकबोली
Nisibis, Nizip नसीबैन
Opporto, Portugal बरतक़ाल (पुरतगाल)
Oran वहरान, ज़ोहरान (अल-जज़ाइर)
Orfa ओरफ़ा
Orontes आसी नदी
Ottoman उसमानी
Oujda वुजदा (मराकश)
Oxus जैहुन/आमू नदी
Palermo बलर्म
Palestine फ़लस्तीन
Pampelona बम्बलूना (अन्दलुस)
Pekin (Cambaluc) ख़ान बालीक़ (पेकिन)
Polay बुलाई
Pelusium, Fermat फ़रमा (मिस्र)
Pergamos बर्गमा, बर्ग़मा, बर्ग़ामुस
Persepolis इस्तख़
Persia फ़ारिस
Phrygia गरमियान
Plato प्लेटो (अफ़लातून)
Pontos बहीरा असवद/बुन्तुस
Prusa ब्रूसा, बुरसू
Ptolemy बतलीमूस
Pyramus जीहान नदी (तुर्की)
Pyrenees जबलुल बरानिस, जबलुल बरतात
Pythagoras फ़ीसाग़ूरस
Quilon कूलुम
Rasi राज़ी
Rayy (Anciant Ragha) रै, राग़ा
Regio रिया
Rhages रै
Rhazes राज़ी
Rhodes रोदस
Rhone रून नदी
Riqqa रिक़्क़ा
Roderic रोडरिक, लज़रीक़
Ramanus Deogenes क़ैसर दिओजनिस
Ronda रुन्दा
Sacralias ज़ुल्लाक़ा (अन्दलुस)
Salamanca ज़लमनका (अन्दलुस)
Samosata समीसात
Sana सनआ
Sancho सांजा (हुक्मरान)
San'a सनआ
Santarem शनतरीन
Santiago de Compostela सेंट यागो, शंत याक़ूब
Saladin सलाहुद्दीन
Saragossa सरक़स्ता (अन्दलुस)
Sardenia सरदानिया (टापू)
Sarus सीहान, सीहून नदी (तुर्की)
Sebastia, Sivas सीवास
Segovia शक़ूबिया
Segura शक़ूरा
Sevilla इशबीलिया
Saint Maria de Algarve संत मारिया, अल-ग़र्ब
Saint Yago सेंट याक़ूब, सेंट यागो
Sicily सक़लिया
Sidon सीदा (लुबनान)
Sidonia शज़ूना
Sierra Nevada सलीद पहाड़, जबलुस-सलज
Silves शलब
Sogdiana सुग़द
Spain, Andalus अन्दलुस, स्पेन
Syracuse सरक़ूसा
Syria शाम, सीरिया
Strait of Gibralter बहरे ज़क़ाफ़
Tagus ताजह
Talavera तलबीरा
Tamerlane तैमूरलंग
Tangier तंजा
Tarifa तरीफ़
Tenes तनिस
Theodomir तदमीर
Thedosiopolis (Karim) कालीक़ला
Thueda तूता (मलका)
Tibrias तबरिया
Tigris दजला (नदी)
Toledo तुलैतिला
Tortosa तरतोशा
Toulousa तलूशा
Trafalgar तरफ़ुत अग़र
Transoxania मावराउन्नहर
Trebizond तराबज़ून
Tripolis तराबुलस
Tunish तूनिस
Tyana तवाना
Tyre सूर
Ukhaidir अल-उख़ैज़िर
Valencia बलंसिया (अन्दलुस)
Venice बुन्दक़िया
Xenil दरियाए शनील
Xeres शरीश, ख़रीस
Yemen यमन
Zamora समूरह
Zaragoza, Saragossa सरक़स्ता, सरक़ुस्ता
Zardalis (Arzachel) ज़रक़ाली
---------------------
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
Subscribe Our You Tube Channel
Recent posts
-
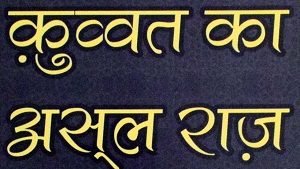
क़ुव्वत का अस्ल राज़
16 March 2024 -

आदाबे ज़िन्दगी
14 March 2024 -
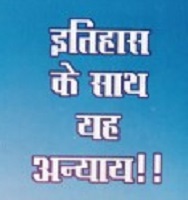
इतिहास के साथ अन्याय
31 March 2020 -

इस्लाम का इतिहास
14 March 2020