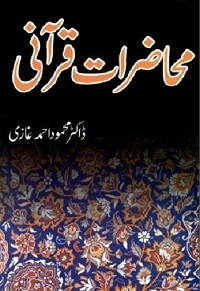
पवित्र क़ुरआन की शिक्षा : आधुनिक समय की अपेक्षाएँ (क़ुरआन लेक्चर -12)
-
कु़रआन (लेख)
- at 12 December 2023
डॉ० महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक: गुलज़ार सहराई
लेक्चर नम्बर-12 (19 अप्रैल 2003)
[क़ुरआन से संबंधित ये ख़ुतबात (अभिभाषण), “मुहाज़राते-क़ुरआनी” जिनकी संख्या 12 है, इनमें पवित्र क़ुरआन, उसके संकलन के इतिहास और उलूमे क़ुरआन (क़ुरआन संबंधी विद्याओं) के कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें यह बताया गया है कि क़ुरआन को समझने और उसकी व्याख्या करने की अपेक्षाएँ क्या हैं, उनके लिए हदीसों और अरबी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ अरबों के इतिहास और प्राचीन अरब साहित्य की जानकारी भी क्यों ज़रूरी है और इस जानकारी के अभाव में क़ुरआन के अर्थों को समझने में क्या-क्या समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। ये अभिभाषण क़ुरआन के शोधकर्ताओं और उसे समझने के इच्छुक पाठकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।]
एक दृष्टि से पवित्र क़ुरआन के दर्स (प्रवचन) की ज़रूरतें और अपेक्षाएँ हर दौर में समान रही हैं। मुसलमानों के इतिहास का कोई दौर ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें उन्हें दर्से-क़ुरआन की ज़रूरत न रही हो, और इसकी अपेक्षाओं और ज़रूरत पर चर्चा न हुई हो। इस्लाम की आरंभिक बारह-तेरह शताब्दियों में कोई शताब्दी ऐसी नहीं गुज़री जब मुसलमानों की शिक्षा-व्यवस्था और उनके प्रशिक्षण-व्यवस्था में पवित्र क़ुरआन को मौलिक और आधारभूत महत्त्व प्राप्त न रहा हो। फिर विभिन्न कालों, विभिन्न ज़मानों और विभिन्न इलाक़ों में मुसलमानों के ज़ेहन में जो सवाल वह्य और नुबूवत (पैग़म्बरी) के बारे में पैदा होते रहे हैं, वे कमो-बेश हर दौर में समान रहे हैं। बल्कि वह्य, नुबूवत (पैग़म्बरी) और मरने के बाद की ज़िन्दगी जैसी मौलिक अवधारणाओं (अक़ीदों) के बारे में नास्तिक जिन सन्देहों एवं आपत्तियों को व्यक्त करते रहे हैं उनकी हक़ीक़त भी हर दौर में कमो-बेश एक जैसी ही रही है। नूह (अलैहिस्सलाम) के ज़माने से लेकर अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के शुभ दौर तक पवित्र क़ुरआन ने विभिन्न लोगों और विभिन्न व्यक्तित्वों का उल्लेख किया है। और उन व्यक्तित्वों के समकालीन लोगों और उनके ज़माने में प्रचलित विचारों और असत्य धारणाओं का खंडन भी किया है। यह ग़लत विचार और असत्य धारणाएँ (अक़ीदे) लगभग एक जैसी ही हैं।
वस्तुतः हर दौर में विशेष कारक और विशेष प्रेरक विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जन्म देते रहे हैं। उदाहरणार्थ एक बड़ी आपत्ति पवित्र क़ुरआन और इससे पूर्व आनेवाली वह्य (ईश-प्रकाशना) पर आम तौर से यह रही है कि इस सन्देश को माननेवाले और इसको लेकर उठनेवाले प्रायः समाज के कमज़ोर और अप्रभावी लोग हैं। समाज के प्रभावशाली और सत्ताधारी लोग ज़्यादातर विरोध ही पर तत्पर रहे। इस वर्ग के हर व्यक्ति के अन्दर यह दंभ होता है कि चूँकि मुझे भौतिक संसाधन प्राप्त हैं और धन-दौलत भी उपलब्ध है, इसलिए बुद्धि एवं विवेक भी मुझे भारी मात्रा में मिला है। यह ग़लतफ़हमी हर दौर के इंसान को रही है। आज भी यह विशाल स्तर पर पाई जाती है कि जिस व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन ज़्यादा हों तो मान लिया जाता है कि बुद्धि एवं विवेक भी उसके पास ज़्यादा है। पवित्र क़ुरआन ने इस आपत्ति का जो जवाब दिया है वह हर दौर और हर ज़माने के लोगों के लिए है।
इसी तरह से एक ख़ास ख़तरा लोगों को यह पैदा हो जाता है कि जब दीन (धर्म) की व्यवस्था आएगी और वह्य पर आधारित सरकार क़ायम होगी तो प्रचलित व्यवस्था बदल जाएगी। फ़िरऔन ने भी यही कहा था कि ये दोनों यानी मूसा और हारून (अलैहिमस्सलाम), तुम्हारी इस आदर्श व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं, जो तुम्हारे यहाँ प्रचलित है। इसकी जगह ये लोग एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। मानो हर वर्तमान और प्रचलित व्यवस्था से कुछ लोगों के हित जुड़े होते हैं। इस व्यवस्था के ध्वजावाहक महसूस करते हैं कि अगर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया गया तो हमारे हित प्रभावित होंगे। इन लोगों के विचार और सन्देह भी एक जैसे ही होते हैं। ज़ाहिर है कि फिर उनके जवाब भी एक जैसे ही होंगे। यही वजह है कि एक दृष्टि से पवित्र क़ुरआन की शिक्षा की आवश्यकता और अपेक्षाएँ हमेशा समान रही हैं।
यह समझना कि आधुनिक काल की अपेक्षाएँ और हैं और प्राचीनकाल की अपेक्षाएँ कुछ और थीं, नासमझी का प्रमाण है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ख़ास हालात में, या विशेष कालों में ख़ास जरूरतों को देखते हुए किसी समय किसी पहलू से कोई ज़रूरत बढ़ जाए या कम हो जाए। जरूरतों में यह कमी-बेशी और अपेक्षाओं में यह आंशिक रद्दो-बदल होता रहता है।
एक समय था कि शिक्षा-व्यवस्था पवित्र क़ुरआन के आधार पर क़ायम थी। तमाम-विज्ञान पवित्र क़ुरआन के हवाले से पढ़े और पढ़ाए जाते थे। जब एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके निकलता था, तो अव्वल तो वह पूरा पवित्र क़ुरआन इस तरह पढ़ चुका होता था जिस तरह एक इस्लामी समाज में पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी से कोई कमी रह भी जाती थी तो शिक्षा-व्यवस्था के विभिन्न अंग उस कमी की भरपाई कर दिया करते थे। उदाहरणार्थ जैसे आज अंग्रेज़ी ज़बान की शिक्षा अनिवार्य है। इसी तरह उस ज़माने में अरबी भाषा की शिक्षा इस्लामी शिक्षा-व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग थी। हर विद्यार्थी इतनी अरबी ज़रूर जानता था कि इस ज़बान को शिक्षा के माध्यम के तौर पर अपना सके और वह इतनी अरबी ज़रूर सीख लेता था कि पवित्र क़ुरआन के टेक्स्ट और व्याख्यात्मक साहित्य को समझने में कम से कम भाषा की हद तक उसको कोई दिक़्क़त न हो। यों उसके लिए पवित्र क़ुरआन का सीखना और आगे चलकर उसके उलूम तक पहुँच प्राप्त कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अब यह बात नहीं रही। आज हमारी शिक्षा-व्यवस्था में ऐसा कोई स्वचालित प्रबंध नहीं है कि उसके परिणामस्वरूप लोग पवित्र क़ुरआन से इस प्रकार परिचित हो जाएँ जिस तरह कि उन्हें परिचित होना चाहिए। इन परिस्थितियों में इस आम अंदाज़ के क़ुरआन के दर्स (प्रवचन) की या शिक्षा-व्यवस्था से हटकर एक बाहरी व्यवस्था के तहत पवित्र क़ुरआन की शिक्षा एवं अध्ययन का महत्त्व अब पहले के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
एक बड़ी वजह तो आधुनिक काल में पवित्र क़ुरआन के आम दर्स के ग्रुपों के महत्त्व की यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि दीन की शिक्षा की कमी की वजह से दीन (धर्म) की अवधारणाएँ और इस्लामी-व्यवस्था में आदेशों एवं निर्देशों का जो क्रम है, सिर्फ़ उसकी समझ में, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में उसका ध्यान रखने में बड़ी ग़लती हो रही है। जब हम कहते हैं कि इस्लाम एक सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्था है तो उसका अर्थ यह है कि इस्लाम में एक सन्तुलन पाया जाता है। और इस्लाम में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में निर्देश मौजूद है। जो व्यक्ति जिस पहलू से अपने जीवन को सहज करना चाहे उस पहलू के लिए पवित्र क़ुरआन में निर्देश मौजूद हैं। उदाहरणार्थ कोई व्यापारी बनना चाहे तो उसके लिए निर्देश मौजूद हैं, कोई शिक्षक बनना चाहे तो उसके लिए मार्गदर्शन मौजूद है और कोई व्यक्ति कोई भी पेशा अरनाना चाहे तो उसके द्वारा अपनाए गए पेशे से संबंधित क्या चीज़ जायज़ है और क्या नाजायज़ है? यह सब पवित्र क़ुरआन में और उसकी टीका एवं व्याख्या यानी हदीसों में, और हदीसों की व्याख्या एवं टीका, यानी फ़िक़्ह और इस्लामी साहित्य और इस्लामी क़ानून के भंडार में मौजूद है। लेकिन अगर जनसाधारण तक इस सन्देश के पहुँचाने और समझाने की कोई व्यवस्था न हो तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कम से कम पवित्र क़ुरआन की शिक्षा को लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके अतिरिक्त जो क्रम इस्लाम की शिक्षा में है उस क्रम को याद दिलाने की कोशिश की जाए। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि दीन (इस्लाम) की मौलिक शिक्षा में जो क्रमिकता है वह क्या है और उस क्रमिकता को नज़र अंदाज़ करने और उसको भूल जाने की वजह से जो ख़राबियाँ समाज में पैदा हो रही हैं, वे क्या हैं।
मुस्लिम समाज के बारे में वैचारिक रूप से यह बात सब लोग जानते हैं कि इसमें दीन और दुनिया का भेद मौजूद नहीं है। इसकी शिक्षा में मूल सिद्धांत तौहीद (एकेश्वरवाद) और एकता (एकत्त्व) है, न केवल दीन और दुनिया की एकता, बल्कि ज्ञान-विज्ञान की एकता, इस्लामी सोच और इस्लामी सभ्यता एवं नागरिकता का आधार है। इस शिक्षा पर पूरी तरह ईमान लाने के अलावा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से जुड़ाव उम्मते-मुस्लिमा (मुस्लिम समुदाय) में एकता की बुनियाद है। इस्लाम की शिक्षा को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उतनी ही मुस्लिम समाज में एकता की सोच पैदा होगी। वैचारिक दृष्टि से तो सब लोग यह बात मानते हैं। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। दीनी (धार्मिक) शिक्षा के बहुत-से केन्द्र ऐसे हैं कि वहाँ से दीन के नाम पर जो शिक्षा आ रही है वह समाज को ‘मसलकों’ (पंथों) और फ़िर्क़ों (वर्गों) के नाम पर विभिन्न हिस्सों में बाँट रही है। अगर थोड़ा-सा ग़ौर करके देखें तो पता चलेगा कि मुस्लिम समाज में पहले से जितने गिरोह या रास्ते मौजूद थे उनमें और बढ़ोतरी हो रही है। जैसे-जैसे मज़हबी शिक्षा का यह ख़ास रंग और अंदाज़ फैल रहा है, उसके साथ-साथ समाज में विभाजन और बिखराव में और बढ़ोतरी हो रही है। अब या तो आप यह कहें कि दीने-इस्लाम और पवित्र क़ुरआन मुसलमानों में एकता का गारंटर नहीं है जो बिलकुल निराधार और वास्तविकता के विरुद्ध बात है। वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ही में कोई कमी है। हम जिस अंदाज़ से दीन की शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मूल रूप से ज़ोर मसलकी रायों और फ़िक़्ही इज्तिहादात पर दिया जाता है। इस रवैये में बहुत कुछ सुधार और पुनरावलोकन की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ दीन के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वे विभिन्न स्तरों की हैं। इन स्तरों को जब तक अपनी जगह पर बरक़रार न रखा जाए उस वक़्त तक इससे वह परिणाम नहीं निकल सकेंगे, जो दीने-इस्लाम पैदा करना चाहता है।
कल ही आप में से किसी ने सवाल किया था कि दीन और मज़हब में क्या फ़र्क़ है? मैंने जवाब में बताया था कि ‘दीन’ से अभिप्रेत अल्लाह तआला द्वारा प्रदान की हुई वह मौलिक शिक्षा है जो आदम (अलैहिस्सलाम) से लेकर आज तक एक ही ढंग से चली आ रही है, जिसमें वक़्त के गुज़रने, हालात के बदलने से कोई कमी-बेशी नहीं होती। दीन के मौलिक आधारों यानी अक़ीदे, तौहीद, रिसालत और आख़िरत पर ईमान, उनकी अपेक्षाओं पर ईमान और अख़्लाक़ (नैतिकता) के सुधार हर दौर में एक ही रहे हैं। क़ौमों के आने-जाने, क़ौमों और समुदायों के उतार-चढ़ाव से उन अक़ीदों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
पवित्र क़ुरआन में लुक़्मान की ज़बान से अदा होनेवाले हिक्मत (तत्त्वदर्शिता) के उल्लेख में भी इस बात की तरफ़ से इशारा मिलता है कि हज़ारों साल पूर्व भी उच्च नैतिक आचरण यही थे जो आज हैं। नैतिक आचरण जो कल थे वे आज भी हैं। और उच्च नैतिक आचरण की जो व्याख्या और टीका अल्लाह तआला के माननेवालों ने विभिन्न कालों में की है वह एक ही रही है और इसमें कोई अन्तर पैदा नहीं हुआ। यही कारण है कि पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षाओं के सार को पवित्र क़ुरआन में बयान करने का। इन उल्लेखों और टिप्पणियों से जो पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षा के बारे में जगह-जगह पवित्र क़ुरआन में बयान किए गया है, यह बात मन में बिठाना अभीष्ट है कि दीन की शिक्षा हर दौर में एक ही रही है। पवित्र क़ुरआन की विभिन्न सूरतों में जहाँ एक ही जगह बहुत-से पैग़म्बरों की शिक्षाओं का ज़िक्र किया गया है वहाँ ग़ौर करने से यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाती है।
पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) के दरमियान शरीअतों (धर्म-विधानों) में फ़र्क़ रहा है। उनके लाए हुए व्यावहारिक आदेशों में हालात और समय का ध्यान हमेशा रखा गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस क़ौम और जिस इलाक़े में जो शरीअत भेजी गई, वह इस क़ौम के स्वभाव, परिवेश और समय की दृष्टि से भेजी गई। कहीं सख़्ती की ज़रूरत थी, कहीं नर्मी की ज़रूरत थी, कहीं अल्लाह के साथ संबंध को मज़बूत करने की ज़रूरत थी। कहीं क़ानूनों के ज़ाहिरी पहलू पर ज़ोर देना ज़रूरी था और कहीं क़ानूनों की मूलात्मा और उनके अंदरूनी पहलू को उजागर करना अभीष्ट था। विभिन्न ज़रूरतें थीं, जिनके हिसाब से शरीअतों का अवतरण हुआ, इसी वजह से उनमें अन्तर का ध्यान रखा गया।
अब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के द्वारा जो शरीअत हम तक पहुँची है, वह रहती दुनिया तक के लिए है। वह हर ज़माने, हर इलाक़े और हर क़ौम के लिए है। वह समय और स्थान से परे है। इसलिए वे तमाम विशेषताएँ जो पिछली शरीअतों में अलग-अलग क़ौमों के लिए ध्यान में रखी गईं, वे सब की सब क़ुरआनी शरीअत में इकट्ठा मौजूद हैं।
हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी तब्लीग़े-दीन (इस्लाम का प्रचार-प्रसार) की है। ग़ैर-मुस्लिमों को और दीन से विमुख मुसलमानों को दीन ही की तब्लीग़ की जाती है। आपने किसी जगह भी इस्लामी साहित्य में ‘तब्लीग़े-शरीअत’ या ‘तब्लीग़े-फ़िक़्ह’ का शब्द नहीं पढ़ा होगा, बल्कि तब्लीग़ और दावत के हवाले से ‘दीन’ ही का शब्द पढ़ा होगा। याद रखिए, तब्लीग़ हमेशा दीन की होती है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने दीन की तब्लीग संसार के कोन-कोने में की। वे चीन तक गए, मध्य एशिया तक पहुँचे और दुनिया में जहाँ-जहाँ तक विजयें प्राप्त हुई हैं वहाँ तक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) पहुँचे और हर जगह दीन ही की तब्लीग़ की। किसी जगह भी किसी फ़िक़्ही मसलक या फ़िक़्ही राय के बारे में यह सवाल नहीं उठाया कि जब ग़ैर-मुस्लिमों को दीन की तरफ़ बुलाएँ तो किस विशेष फ़िक़्ही राय की तरफ़ बुलाने की कोशिश करें। किसी फ़िक़्ही या कलामी (तार्किक) राय के बजाय उन्होंने दीन की बुनियादों ही की तरफ़ बुलाया। यानी अल्लाह तआला के एकत्व, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की नुबूवत (पैग़म्बरी), आख़िरत के दिन के प्रतिदान और दंड और नैतिक आचरण का सुधार। यही चीज़ें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और इस्लाम के मुख्य दौर में इस्लाम की ओर आह्वान करनेवालों की दावत का विषय हुआ करती थीं।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जो व्यवस्था लेकर आए हैं उसका पालन करना निस्सन्देह अपरिहार्य है, और यह चीज़ नुबूवत (पैग़म्बरी) की परिकल्पा में शामिल है। इसके अलावा प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने किसी फ़िक़्ही, कलामी या तफ़सीली (विस्तृत) मामले की तरफ़ किसी का आह्वान नहीं किया। दावत केवल दीन की दी जाती है। दावते-शरीअत या दावते-फ़िक़्ह कभी नहीं हुई। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दरमियान फ़िक़्ही या कलामी मामलात में कोई मतभेद नहीं हुआ करता था। उनके दरमियान मतों की भिन्नता निस्संदेह मौजूद थी। किसी ख़ास फ़िक़्ही मामले के बारे में किसी सहाबी की एक राय थी और किसी और सहाबी की दूसरी राय थी। कुछ सहाबा समझते थे कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है। लेकिन कुछ सहाबा का ख़याल था कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू नहीं टूटता। अब यह एक फ़िक़्ही राय है। एक बुज़ुर्ग के ख़याल में इससे वुज़ू टूटता है और दूसरे बुज़ुर्ग के ख़याल में नहीं टूटता। यह मतभेद दीन में नहीं है। फ़िक़्ही आदेशों में है। एक सहाफ़ी बयान किया करते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस सुनी है कि मय्यत पर रोने से मय्यत को अज़ाब होता है। किसी ने जाकर आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से बयान किया। उन्होंने कहा, बिलकुल ग़लत, किसी की ग़लती की सज़ा कोई दूसरा कैसे भुगत सकता है। पवित्र क़ुरआन में तो आता है اَلَاتَزِرُ وَازِرَۃً وِزْرَ اُخْرٰی यानी “कोई बोझ उठानेवाला किसी और का बोझ न उठाएगा।” (क़ुरआन, 53:38)
यानी ऐसी अनगिनत मिसालें हैं कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दरमियान किसी क़ुरआनी या हदीसे-रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को समझने में मतभेद हुआ। एक सहाबी ने शरीअत के आदेश को एक तरह समझा और दूसरे सहाबी ने दूसरी तरह समझा। दोनों ने अपनी भरसक समझ और विवेक के अनुसार अतंयत निष्ठापूर्ण ढंग से क़ुरआन और हदीस की ‘नुसूस’ (स्पष्ट आदेशों) को समझने की कोशिश की। कभी-कभी जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सामने इस प्रकार का विवादित मामला पेश किया गया तो भी तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक राय के बारे में कहा कि यह दुरुस्त है और दूसरी राय की ग़लती स्पष्ट कर दी। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ग़लतीवाली राय को छोड़ दिया गया और सही आदेश पर सबने मतैक्य कर लिया। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने दोनों की रायों को एक साथ दुरुस्त क़रार दिया और दोनों पक्षों से कहा कि तुमने भी दुरुस्त किया और तुमने भी दुरुस्त किया।
एक छोटी-सी मिसाल पेश करता हूँ। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब के बाद जब इस्लाम-विरोधी वहाँ से चले गए तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़ैसला किया कि क़बीला बनू-क़ुरैज़ा के यहूदियों को सज़ा दी जाए। जिन्होंने अंदर से बग़ावत और ग़द्दारी की कोशिश की थी। आपने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से कहा, “तुममें से कोई व्यक्ति बनू-क़ुरैज़ा के इलाक़े में पहुँचने से पहले हरगिज़ अस्र की नमाज़ न पढ़े।” इस मौक़े पर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की संख्या 1500 के क़रीब थी। सबको यही निर्देश था कि तुममें से कोई व्यक्ति हरगिज़ उस वक़्त तक अस्र की नमाज़ अदा न करे जब तक बनू-क़ुरैज़ा के इलाक़े में न पहुँच जाए। अब आप देख लीजिए कि यह बहुत अधिक ताकीद का हुक्म है। इस ताकीद का स्पष्ट अर्थ यह है कि इसके अलावा करने की बिलकुल गुंजाइश नहीं है, अस्र की नमाज अवश्य ही वहीं जाकर अदा करनी है।
यह स्पष्ट और दोटूक आदेश सुनकर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) प्रस्थान कर गए। कोई गिरोह किसी रास्ते से रवाना हो गया और कोई और ग्रुप किसी और रास्ते से। जब रास्ते में अस्र का वक़्त तंग होने लगा तो कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने कहा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का मक़सद यह नहीं था कि अस्र की नमाज़ देर से पढ़ना या छोड़ दिना, बल्कि मक़सद यह ताकीद करना था कि अस्र से पहले वहाँ पहुँचना है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की एक बड़ी संख्या का यह दृष्टिकोण था, यानी इस मौक़े पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के आदेश की व्याख्या में मतभेद पैदा हुआ। और प्रकट में यानी ज़ाहिरी शब्दों के लिहाज़ से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की एक जमाअत ने आदेश का उल्लंघन किया और नमाज़ रास्ते में पढ़ ली। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि “हम नहीं जानते कि अस्र का वक़्त कौन-सा है और मग़रिब का वक़्त कौन-सा है। हमसे उन्होंने पहले ही कहा था कि अस्र अमुक समय पर पढ़ा करो, आज उनका ही कहना है कि अस्र वहाँ जाकर पढ़ो, इसलिए हम तो वहीं जाकर पढ़ेंगे।” हम कह सकते हैं कि यह व्याख्या का यह ढंग मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के प्रति उन सहाबा के अति प्रेम को दर्शाता है और वह दूसरी व्याख्या बुद्धिसंगत व्याख्या है। चुनाँचे एक ग्रुप ने अस्र की नमाज़ क़ज़ा की और बनू-क़ुरैज़ा के इलाक़े में जाकर ही अदा की। अगले दिन दोनों ग्रुप अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में हाज़िर हुए और सारी स्थिति आपके सामने पेश की। आपने दोनों से कहा, “तुमने ठीक किया।” यों दोनों के तरीक़े को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने पसंद किया और किसी को भी ग़लत नहीं कहा।
यह वह चीज़ है जिसको आप शरीअत की समझ कहते हैं। यह शोध, फ़तवा (धर्मादेश) और पठन-पाठन का विषय तो होगी, लेकिन इस्लाम के प्रचार-प्रसार का विषय नहीं होगी। जब इस्लाम की ओर आह्वान किया जाएगा तो वह सिर्फ़ दीन (धर्म) की ओर बुलाया जाएगा। और तब्लीग़ होगी तो सिर्फ़ दीन की होगी। जो लोग दीन को स्वीकार कर लेंगे उनको शिक्षा के द्वारा शरीअत के आदेश बताए जाएँगे। यह शिक्षा, शरीअत की शिक्षा होगी। जो लोग मुसलमान होते जाऐंगे, उनके लिए शरीअत की शिक्षा की ज़रूरत पेश आती जाएगी। इस तरह शरीअत के तमाम विवरण सामने आएँगे, जो दीन के बाद का चरण है।
इसके बाद शरीअत के आदेशों को समझने में एक से अधिक मत हो सकते हैं। जैसा कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दरमियान थे। जब यह चरण आएगा तो शोध का सवाल पैदा होगा। शोध के विषय और इसके परिणाम सिर्फ़ शोधकर्ताओं की दिलचस्पी के विषय होते हैं। एक विद्वान या फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) के शोध में एक अर्थ सही है और दूसरे की निगाह में दूसरा अर्थ सही है। इस हदीस से पता चला कि एक साथ दो अर्थ भी सही हो सकते हैं। हमारे विश्वास और अन्तर्दृष्टि की हद तक एक अर्थ सही है, और दूसरे फ़क़ीह की समझ और अन्तर्दृष्टि की हद तक दूसरा अर्थ सही है। इसकी संभावना हर वक़्त मौजूद है कि हमारी राय सही न हो, दूसरी राय सही हो और यह कोई बुरी बात नहीं है। इसको भी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बयान किया कि अल्लाह तआला ने जहाँ शरीअत के आदेश अवतरित किए, बहुत-से मामलों को फ़र्ज़ क़रार दिया, बहुत-सी चीज़ों को हराम ठहार दिया, वहीं बहुत-सी बातों के बारे में ख़ामोश रहे, यानी दया और स्नेह के कारण कुछ चीज़ों के बारे में आदेश अवतरित नहीं किया। यानी इस बात की आज़ादी दी गई कि इन सीमाओं के अन्दर-अंदर तुम अपनी समझ और अन्तर्दृष्टि के अनुसार फ़ैसला करो और जिस नतीजे पर पहुँचो उसपर अमल करो।
उदाहरण के तौर पर एक सहाबी हाज़िर हुए और कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग रेगिस्तान के रहनेवाले हैं, वहाँ पानी की कमी होती है। किसी जगह गढ़े या तालाब में अगर पानी जमा हो और हमें मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी नेमत होती है। लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता कि इस पानी में किसी दरिंदे ने मुँह तो नहीं डाल दिया, इसमें कोई गन्दगी तो नहीं गिर गई, मालूम नहीं कि वह पानी हमारे लिए पाक भी होता है या नहीं। हमें ऐसे मौक़े पर क्या करना चाहिए।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जवाब में कहा, الماءالکثیر لاینجس “ज़्यादा पानी नापाक नहीं होता।” आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ‘अफ़सहुल-अरब’ (अरबों में सबसे अच्छी भाषा बोलनेवाले) थे। आपसे ज़्यादा उत्कृष्ट भाषा बोलनेवाला, दुश्मनों की स्वीकारोक्ति के अनुसार भी अरब द्वीप में कोई पैदा नहीं हुआ। आपको मालूम था कि सवाल करनेवाला चाहता क्या है। तो आपने सायास वह शैली प्रयोग की जिसकी अनगिनत व्याख्याएँ हो सकती हैं।
सहाबा और ताबिईन के बाद जब आदेश किताबी रूप में संकलित होने लगे तो यह सवाल पैदा हुआ के ‘अल-माउलकसीर’ से क्या मुराद है। कितने पानी को ‘अल-माउलकसीर’ (ज़्यादा पानी) कहेंगे। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) मदीना मुनव्वरा के रहनेवाले थे, जहाँ सिर्फ दो या तीन कुएँ मौजूद थे। अतः उनके ख़याल में ‘अल-माउलकसीर’ (ज़्यादा पानी) से मुराद इतना पानी था जो बड़े दो मटकों में आ जाए। इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) कूफ़ा के रहनेवाले थे जहाँ एक तरफ़ दजला नदी बह रही थी और दूसरी तरफ़ फ़ुरात नदी थी। पानी की कोई कमी नहीं थी। अतः उनके ज़ेहन में ज़्यादा पानी की जो कल्पना आई वह यह थी कि अगर पानी का इतना बड़ा तालाब हो कि अगर एक तरफ़ से इस का पानी हिलाया जाए तो दूसरी तरफ़ का पानी न हिले वह ‘अल-माउलकसीर’ (ज़्यादा पानी) है। लुग़त में इन दोनों अर्थों की गुंजाइश है। हदीस के शब्दों में दोनों की गुंजाइश है।
यह तो हो सकता है और लगातार होता रहा है कि कोई विद्वान अपनी समझ अपनी पड़ताल और अपने प्रमाण से एक राय के बारे में यह राय क़ायम करे कि यह मुझे ज़्यादा सही और दुरुस्त मालूम होती है। और दूसरी राय सही मालूम नहीं होती, या विपरीत, लेकिन बहरहाल शोध का विषय है और शोध का विषय रहना चाहिए। इससे बहस फ़िक़्ह, उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों के क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। एक विद्वान अपने दिल से शोध करेगा और उसके अनुसार राय को क़ायम करेगा। यह न आम और आरंभिक शिक्षा का विषय है न तब्लीग़ का और न इस्लामी आह्वान का। यह कभी नहीं हुआ कि इस्लाम के किसी फ़क़ीह ने खड़े होकर यह एलान किया हो कि “ऐ इराक़वालो ख़बरदार! अहमद-बिन-हम्बल का अमुक शोध ग़लत है, अतः इस मामले में उनकी बात मत मानना। या किसी एक फ़क़ीह ने खड़े होकर भी दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी की हो। इन लोगों ने इन उत्कृष्ट कलात्मक और शोधात्मक विषयों को शोध के दायरे तक सीमित किया और जब भी आह्वान किया ‘दीन’ की ओर किया, जो तमाम पैग़म्बरों के ज़माने से एक ही चला आ रहा है। और दीन का यही आह्वान मुस्लिम समुदाय की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
जब लोग इस्लाम की परिधि में प्रवेश कर जाएँ तो उन्हें शरीअत (धर्म-विधान) की शिक्षा दी जाएगी। जो लोग शरीअत के आदेशों का पालन करने लग जाएँगे, तो व्यावहारिक मामलों में इस प्रकार के विवरणों में जहाँ एक से अधिक रायें पाई जाती हैं, वहाँ वह शोधकर्ताओं से सम्पर्क करेंगे और जिस विद्वान तथा ईशभय रखनेवाले के शोध से वे सहमत होंगे उसके शोध को स्वीकार कर लेंगे।
शोध के बाद एक चीज़ और होती है जो किसी ख़ास विद्वान की प्रवृत्ति होती है। इस्लाम ने किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं किया, हर व्यक्ति की रूचि और स्वभाव विभिन्न होता है। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में हर प्रवृत्ति के लोग मौजूद थे। कुछ ऐसे लोग थे जो हर चीज़ को बड़े तार्किक और बौद्धिक ढंग से देखते थे। और कुछ लोग थे जिनका अंदाज़ बड़ा श्रद्धापूर्ण था, उनके यहाँ प्रेम की भावनाएँ पाई जाती थीं। एक बार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मस्जिदे-नबवी में ख़ुतबा दे रहे थे। कुछ लोग खड़े हुए थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उनसे संबोधित होकर कहा कि जो लोग खड़े हैं वे बैठ जाएँ। मस्जिद से बाहर गली में चलते हुए कुछ ऐसे लोगों के कान में आपकी आवाज़ पड़ी जो अभी मस्जिद में दाख़िल नहीं हुए थे। वह उस वक़्त एक जगह गली में बैठ गए। ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का संबोधन तो उन लोगों के लिए था जो मस्जिद में मौजूद थे। जो लोग अभी मस्जिद से बाहर थे यह निर्देश उनके लिए न था। लेकिन उन्होंने दिल में कहा होगा कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे कानों में तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आवाज़ आई कि बैठ जाओ और हम बैठ गए। यह एक प्रेममयी अंदाज़ है। यह दोनों दो विभिन्न स्वभावों के नमूने हैं।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में निस्सन्देह प्रवृत्ति का मतभेद मौजूद था। किसी सहाबी की प्रवृत्ति थी कि ज़िंदगी-भर तलवार लेकर मैदाने-जंग में जिहाद करते रहें और कभी पठन-पाठन का कार्य नहीं किया। मिसाल के तौर पर ख़ालिद-बिन-वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ज़िंदगी मैदाने-जंग ही में गुज़ार दी। कभी कोई दर्स का ग्रुप क़ायम नहीं किया। कभी हदीसों का उल्लेख करने के लिए नहीं बैठे। वह मैदाने-जिहाद के शहसवार थे, उनकी प्रवृत्ति तलवार चलाने में थी। वह ज़िंदगी भर इसी मैदान में दीन की सेवा करते रहे। इसके विपरीत कुछ दूसरे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की प्रवृत्ति थी कि ज़िंदगी-भर दर्से-हदीस देते रहे और नाम मात्र ही कभी तलवार उठाई, जैसे अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु)। उन्होंने कभी कोई शहर फ़तह नहीं किया। जिहाद का महत्त्व अपनी जगह और हदीस के प्रचार-प्रसार का महत्त्व अपनी जगह। ख़ालिद-बिन-वलीद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कभी यह नहीं कहा कि अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) को देखो जिहाद के फ़ज़ाइल (महत्ता) जानता है फिर भी कभी तलवार नहीं उठाता, कभी जिहाद में हिस्सा नहीं लेता। और न ही कभी अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा कि ख़ालिद-बिन-वलीद ने हदीस की कोई सेवा नहीं की। तो अपनी-अपनी प्रवृत्ति थी। किसी के अंदर कोई प्रवृत्ति थी और किसी के अंदर कोई। हाँ कुछ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) थे जिनके अंदर बड़ी व्यापकता पाई जाती थी। हर दौर में व्यापकता रखनेवाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। इस्लाम इसलिए नहीं आया कि लोगों की प्रवृत्ति को बदलकर रख दे। इस्लाम का काम लोगों की प्रवृत्ति को बढ़ाना और व्यक्तियों की प्रतिभाओं को उभारना है। इस्लाम की सच्ची भावना हर व्यक्ति से उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार काम लेती है।
कभी-कभी इसी प्रवृत्ति की वजह से किसी धार्मिक व्यक्तित्व का एक स्वभाव बन जाता है। उसके माननेवालों, शिष्यों और शागिर्दों में से बहुत-से लोग उसकी प्रवृत्ति की पैरवी करने लगते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आपने जिससे दीन सीखा है अगर वह आपका आदर्श और रोल मॉडल है तो अगर आप उसकी प्रवृत्ति को अपनाना चाहें तो इसमें कोई हरज नहीं है, बशर्तिके वह दीन की शिक्षाओं के अंदर-अंदर हो, लेकिन अगर आप दूसरों से भी यह माँग करना शुरू कर दें कि सब उस व्यक्तित्व की प्रवृत्ति की पैरवी करें और इसकी प्रवृत्ति का प्रचार करना शुरू कर दें तो ग़लत होगा। प्रवृत्ति तो किसी सहाबी की भी अनुकरणीय नहीं है यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की निजी पसन्द के बारे में भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की निजी पसन्द है, जिसका जी चाहे अपनाए और जिसका जी चाहे इसको न अपनाए।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की निजी प्रवृत्ति की भी मिसाल पेश कर देता हूँ। एक बार आप दस्तरख़्वान पर बैठे थे। कोई ख़ास क़िस्म का गोश्त दस्तरख़्वान पर मौजूद था। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उसे खाने से परहेज़ किया और उसके बाद कहा कि मेरी तबीअत उसे खाने की इजाज़त नहीं देती। जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इस दस्तरख़्वान पर आपके साथ खाने में शरीक थे, उन्होंने इस गोश्त को खाया और आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की प्रवृत्ति की पैरवी करने को ज़रूरी नहीं समझा।
यानी प्रवृत्ति की पैरवी अपने शौक़ की चीज़ है। जिसे शौक़ हो वह प्रवृत्ति की पैरवी करे और जिसे न हो न करे। यह तब्लीग़ और दावत का विषय नहीं है। इस की तब्लीग़ नहीं करनी चाहिए।
यों ये चार चीज़ें, दीन, शरीअत, फ़िक़्ह और ज़ौक़ (प्रवृत्ति) हमारे सामने आती हैं। उनमें प्रचार-प्रसार केवल दीन का होगा। शरीअत की आम शिक्षा और फ़िक़्ह की उच्च शिक्षा होगी। यह लम्बी भूमिका मैंने इसलिए बाँधी कि जब हम क़ुरआन के दर्स (शिक्षा) की मजलिसें आयोजित करें तो हमारे सामने दर्से-क़ुरआन के केवल पहले दो उद्देश्य होने चाहिएँ, यानी जो लोग दीन का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते उनके सामने सिर्फ़ दीन की बुनियादी बातों को रखें। दीन के अक़ीदे (अवधारणाएँ), इस्लाम की नैतिक विशेषताएँ और दीन की पूरा व्यवस्था उन्हें बताने की ज़रूरत है। अगर संबोधित वे लोग हैं जो दीन से तो जुड़े हैं, लेकिन उन्हें शरीअत के इल्म की ज़रूरत है तो शरीअत का इल्म उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और पवित्र क़ुरआन की आयतों की रौशनी में पहुँचाना चाहिए। पवित्र क़ुरआन में जो चीज़ संक्षेप में आई है, हदीस में उसका विवरण आ गया है। उदाहरणार्थ पवित्र क़ुरआन में ‘तय्यिबात’ और ‘ख़बीसात’ का ज़िक्र है। अब इनसे कौन-सी चीज़ें अभिप्रेत हैं और उनकी पहचान क्या हैं। यह सब विवरण हदीस में मौजूद है। पवित्र क़ुरआन में है कि अल्लाह तआला ने ‘फ़ुहशा’ और ‘मुनकर’ को हराम क़रार दिया है। अब क्या ‘फ़ुहशा’ है और क्या ‘मुनकर’ है। यह सब विवरण हदीस में मिलेगा। यह सब चीज़ें शरीअत का आधार हैं और य़े पवित्र क़ुरआन में शामिल हैं।
हमारे दर्से-क़ुरआन के यही दो उद्देश्य हैं। हो सकता है कि आपके कुछ संबोधितगण केवल पहली सतह के संबोधित हों। अफ़सोस कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ‘दीन’ की मौलिक बातों से भी अवगत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि दीन की मौलिक शिक्षाएँ उन तक पहुँचाएँ और किसी अनावश्यक बहस में न पड़ें।
अगर आपके संबोधित ऐसे लोग हैं जो दीन के बुनियादी अक़ीदों से तो अवगत हैं, लेकिन उन्हें शरीअत के बुनियादी मामलों की जानकारी नहीं है तो दर्से-क़ुरआन के दौरान में शरीअत की शिक्षा की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे संबोधितों को शरीअत की शिक्षा भी दी जाए। लेकिन किसी ऐसे मामले को न उठाया जाए जिसमें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम), बड़े इमामों और इस्लामी विद्वानों के दरमियान एक से ज़्यादा मत रहे हों। किसी राय के बारे में यह कहना कि सिर्फ़ यही सही है बाक़ी सब ग़लत है, यह दीन और शरीअत दोनों के स्वभाव के ख़िलाफ़ है।
ख़ुद शरीअत ने इस बात की गुंजाइश रखी है कि कुछ आदेशों में एक से अधिक रायें हों। ऐसा इसलिए है कि शरीअत समय और स्थान से परे है। संभव है कि एक व्याख्या कुछ ख़ास हालात में अधिक सन्दर्भानुकूल हो और दूसरी व्याख्या दूसरे हालात में अधिक उचित साबित हो। इसी तरह टीका एवं व्याख्याएँ भी बदलती रहती हैं।
उदाहरण के तौर पर पवित्र क़ुरआन में यहूदियों के सन्दर्भ में आया है कि ये वे लोग हैं जो अल्लाह तआला की आयतों को कुछ सिक्कों के बदले बेच डालते हैं, (یِشترون با یٰتی ثمناً قلیلا) जिस ज़माने में प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम), ताबिईन और तबा-ताबिईन का ज़माना था, और एक से एक परहेज़गार व्यक्ति मौजूद था, उन्होंने उसका अर्थ यह लिया कि जो पवित्र क़ुरआन पढ़ाने पर पारिश्रमिक लेता है वह जायज़ नहीं है। निस्सन्देह उन्होंने अपने ज़माने के लिहाज़ से इस आयत का बिल्कुल ठीक अर्थ लिया। लेकिन फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि लोगों ने महसूस किया कि अगर पवित्र क़ुरआन पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को कारोबार और रोज़गार के झमेलों से मुक्त न किया जाए और उन्हें इस सेवा का पारिश्रिमक न दिया जाए तो पवित्र क़ुरआन की शिक्षा रुक जाएगी। इसलिए कि पहले जिस तरह लोग स्वैच्छिक रूप से इस काम को किया करते थे, इस भावना से इस काम के करनेवाले अब नहीं रहे। जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि कुछ फ़ुल टाइमवाले कर्मचारी हों, जिनका कोई और काम न हो और वह पवित्र क़ुरआन की शिक्षा दिया करें। उन्होंने पवित्र क़ुरआन की एक और आयत से और अन्य ‘नुसूस’ (स्पष्ट आदेशों) से यह राय क़ायम की कि इस तरह के लोगों को उनका काम सिर्फ़ क़ुरआन की शिक्षा देना हो और वे दर्से-क़ुरआन की व्यस्तता के कारण कोई और काम न कर सकते हों, उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है और इस काम का यह पारिश्रमिक उन आयतों की वईद (अज़ाब की धमकी) में नहीं आएगा जहाँ पवित्र क़ुरआन की आयतों पर क़ीमत लेने का उल्लेख हुआ है। अब देखिए कि एक ही आयत है, लेकिन दो विभिन्न व्याख्याएँ दो समयों की दृष्टि से इसी एक आयत से ली गई हैं।
मान लीजिए कि अगर बाद के फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्री) यह व्याख्या न निकालते तो आज कितने लोग होते जो बिना पारिश्रमिक यह काम करने के लिए तैयार होते, और पवित्र क़ुरआन कुल वक़्ती तौर पर पढ़ाया करते। ऐसे निस्स्वार्थ लोगों की अनुपस्थिति में पवित्र क़ुरआन की शिक्षा कितनी सीमित होकर रह जाती। आज मसजिदों में जगह-जगह क़ुरआन की शिक्षा हो रही है। दीनी मदरसे और उच्च शिक्षा के संस्थान खुले हुए हैं और टीचरों को वेतन भी मिल रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो सका कि बाद के क़ुरआन के मुफ़स्सिरीन (टीकाकारों) ने अपने ज़माने की अपेक्षाओं और व्याख्याओं का ध्यान रखकर क़ुरआनी आयतों की व्याख्या की जो नए हालात में अधिक व्यावहारिक थी।
आज इमाम अबू-हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) जैसे लोग मौजूद नहीं हैं। वह फ़िक़्ह का दर्स दिया करते थे। उनके मकतब के सामने एक नानबाई की दुकान थी। एक ग़रीब और विधवा औरत अपना बच्चा नानबाई की दुकान पर बिठा गई कि यह यहाँ मज़दूरी भी करेगा और काम भी सीखेगा। नानबाई ने उससे रोज़ाना की थोड़ा-सी मज़दूरी भी तय कर ली। बच्चे का नानबाई की दुकान पर दिल नहीं लगा और वह वहाँ से भागकर इमाम साहब के दर्स के ग्रुप में जा बैठा। जब माँ बच्चे की ख़ैर-ख़बर लेने के लिए नानबाई की दुकान पर गई तो पता चला कि बच्चा तो नानबाई के पास आने के बजाय इमाम साहब के दर्स में जाकर बैठता है। माँ इमाम साहब के घर गई और बच्चे को डाँट-डपटकर दोबारा नानबाई की दुकान पर बिठाकर चली गई। बच्चा एक बार फिर भागकर चला गया। दूसरी बार जब माँ बच्चे को लेने गई तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या माजरा है। बच्चे की माँ ने शिकायत की कि ग़रीबी और परेशानी की वजह से बच्चे को रोज़गार में लगाना चाहती हूँ, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से यह काम नहीं सीखता। इमाम साहब ने उस महिला को अपने पास से एक बड़ी रक़म दी और आगे के लिए अपने पास से वज़ीफ़ा (गुज़ारा भत्ता) तय कर दिया। महिला से कहा कि बच्चे को उनके मकतब में बैठने दिया जाए। वज़ीफ़ा बहुत पर्याप्त था। इसलिए माँ ने स्वीकृति दे दी और बच्चा इमाम साहब के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगा। यहाँ तक कि वह बच्चा बड़ा होकर क़ाज़ी अबू-यूसुफ़ बना। वह इस्लामी इतिहास के पहले ‘क़ाज़िउलक़ज़ा’ (न्यायाधीश) बने और उनकी किताब ‘किताबुल-ख़िराज’ आर्थिक क़ानून पर दुनिया की पहली किताब है।
इस तरह के लोग आज मौजूद नहीं हैं। अगर इस्लामी विद्वान और फ़क़ीह लोग पिछले फ़तवों और तफ़सीर (टीका) पर जमे रहते तो आज दर्सो-तदरीस (पठन-पाठन) के लिए लोग कहाँ से आते। कहने का मक़सद यह है कि दीन के कुछ आदेशों की व्याख्या और टीका इस्लामी फ़ुक़हा अपने-अपने हालात और अपने-अपने ज़मानों की दृष्टि से करते चले आए हैं, इसलिए किसी एक राय के आधार पर मुसलमानों को ग़लत और गुनाहगार कहना दुरुस्त नहीं। ऐसे मामलों के आधार पर जो मुस्लिम समुदाय के लिए फ़ायदेमन्द हैं अगर मुस्लिम समुदाय में फूट पैदा कर दी गई तो जो चीज़ मुस्लिम समुदाय की सुविधा के लिए भेजी गई थी वह फूट का ज़रिया बन जाएगी। और यह दीन के स्वभाव के ख़िलाफ़ है।
उम्मत (मुस्लिम समुदाय) की एकता तो कुरआन के स्पष्ट आदेश से साबित है, وَ اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ अर्थात् “और निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूँ। अतः मेरा डर रखो।” (क़ुरआन, 23:52) यह आयत पवित्र क़ुरआन में इन्ही शब्दों के साथ कई बार आई है। फिर उम्मत की दुआ तो इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने माँगी है رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ अर्थात् “ऐ हमारे रब! हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना और हमारी संतान में से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय बना, और हमें हमारे इबादत के तरीके बता और हमारी तौबा क़ुबूल कर। निस्संदेह तू तौबा क़ुबूल करनेवाला, अत्यंत दयावान है।” (क़ुरआन, 2:128) जो उम्मत (समुदाय) पवित्र क़ुरआन के स्पष्ट आदेश से, इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ से और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रात-दिन की मेहनत से क़ायम हुई है, जिसकी एकता और सुरक्षा की दुआएँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने रातों को जागकर माँगी हैं, क्या उसकी एकता को किसी ऐरे-ग़ैरे की राय के आधार पर बिखराव का शिकार कर दिया जाए? यह सरासर शरीअत के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि कि हमने इस्लाम की ओर आह्वान, शिक्षा, शोध और प्रवृत्ति इन चारों चीज़ों को आपस में गड्ड-मड्ड कर दिया है। शोध और प्रवृत्ति की न दावत होती है और तब्लीग़ होती है। जो अपनी प्रवृत्ति की ओर बुला रहा है वह ग़लत कर रहा है। वह एक ऐसी चीज़ लोगों पर थोप रहा है जिसकी ओर कभी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी नहीं बुलाया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने नहीं कहा कि गोह का गोश्त खाना मुझे पसन्द नहीं है, अतः तुम कभी मत खाओ। इसलिए ऐसे मामलों में बहुत सावधानी की ज़रूरत है।
यह तो इस मक़सद की बात थी जिसके लिए हमें दर्से-क़ुरआन के ग्रुप बनाने हैं। लेकिन लोगों को दीन के बुनियादी अक़ीदों पर जमा करना और शरीअत की शिक्षा इस तरह देना कि जहाँ-जहाँ ख़ुद अल्लाह ने मतभेद की गुंजाइश रखी है, उस मतभेद को आप स्वीकार करें।
अब होता यह है जो बिलकुल दुरुस्त नहीं है कि एक आलिम का दर्से-क़ुरआन होता है, इसमें सिर्फ़ उस ख़ास मसलक के लोग होते हैं जो उन आलिम का अपना फ़िक़्ही या कलामी मसलक होता है। दूसरे मसलक का कोई आदमी दर्शकों या श्रोताओं में मौजूद नहीं होता। क़ुरआन का अनुवाद भी अपने मसलक ही के आलिम का ख़ास होता है। यों तो किसी अनुवाद या तफ़सीर को ख़ास कर लेने में कोई हरज नहीं है। बल्कि एक दृष्टि से बेहतर और उचित यही है जिससे आपकी प्रवृत्ति मिले उसी आलिम के अनुवाद और टीका को आप पढ़ लें। लेकिन अगर इससे आगे बढ़कर यह कहा जाए कि अमुक अनुवाद और टीका ही को पढ़ा जाए, उसके सिवा किसी और अनुवाद या टीका को न पढ़ा जाए तो यह बात ग़लत होगी। किसी को इस बात का हक़ नहीं बनता कि लोगों को ज़बरदस्ती अपनी प्रवृत्ति पर इकट्ठा करे।
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो उन लोगों के सामने क़ुरआन का दर्स दे रहे हैं जो व्यावहारिक मुसलमान हैं और दीन की बुनियादी बातों से अवगत हैं। ऐसे श्रोताओं को शरीअत के आदेश और विवरण जानने की ज़रूरत होती है। अब जो लोग शरीअत की शिक्षा दे रहे हैं और किसी ऐसे मामले पर पहुँचते हैं जहाँ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) का मतभेद नज़र आता है तो दर्स में किसी ख़ास राय के विशेषकर समर्थन और दूसरी रायों के विशेषकर खंडन से बचना चाहिए और इस मतभेद की गुंजाइश रखनी चाहिए। इसलिए कि ख़ुद फ़ुक़हा ने इस मतभेद को बरक़रार रखते हुए दूसरे दृष्टिकोण के सम्मान का ध्यान हमेशा रखा है और बराबर इसपर ज़ोर दिया है कि हमारी एक राय है और हमें अपने इल्म और अन्तर्दृष्टि के आधार पर पूरा यक़ीन है कि यह राय सही है। लेकिन इस राय के ग़लत होने की संभावना बहरहाल मौजूद है। इसी तरह से वह राय जो किसी दूसरे आदरणीय फ़क़ीह की है हम उसको अपनी अत्यंत गहरी समझ के अनुसार सही नहीं समझते, लेकिन उसके सही होने की संभावना बहरहाल मौजूद है। इस्लामी फ़ुक़हा की यही सोच रही है और यही अंदाज़ रहा है।
इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) और इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) के दरमियान बहुत-से मामलों में मतभेद है। उनके अनुयायियों के दरमियान हमेशा से बहसें जारी हैं। अन्य फुक़हा के दरमियान भी बहसें होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन उनमें से किसी फ़क़ीह ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने जो राय क़ायम की है यही दीन है और यही शरीअत है। इन लोगों का कहना यह होता था कि यह मेरी समझ है, इसके अनुसार मैंने शरीअत को समझा है। दीन की बुनियादों और ज़रूरतों में किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता शरीअत के कुछ आदेशों में मतभेद की गुंजाइश रखी गई है। इस मतभेद में उनका रवैया क्या होता था इसका अंदाज़ा इससे लगइए—
इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) यह समझते थे कि फ़ज्र की नमाज़ में दूसरी रकअत में रुकू से खड़े होकर ‘क़ुनूत’ (एक विशेष दुआ) पढ़ा जाना चाहिए। वह फ़ज्र की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ने को अनिवार्य समझते थे, और आज भी जहाँ-जहाँ शाफ़िई मसलक के माननेवालों की बहुलता है जैसे इंडोनेशिया मलयेशिया और मिस्र वग़ैरा, वहाँ फ़ज्र की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ा जाता है। एक अजीब रंग होता है जब इमाम क़ुनूत पढ़ता है और लोग आमीन कहते हैं तो एक अजीब समाँ होता है। ऐसा लगता है कि अंदर से दिल हिल रहा है।
इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) इसको सही नहीं समझते। उनकी राय में जिन हदीसों से फ़ज्र की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ा जाना मालूम होता है वह एक ख़ास घटना से संबंधित थीं, उनसे कोई स्थायी आदेश साबित नहीं होता। एक बार इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) का बग़दाद आना हुआ। उनके ठहरने दौरान में एक रोज़ उन्हें उस जगह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ानी थी, जहाँ इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) दर्स दिया करते थे। यह मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं थी। उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में बनाई गई थी और अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रहमतुल्लाह अलैह) जैसे प्रतिष्ठित सहाबी वहाँ दर्स (क़ुरआन की शिक्षा) दिया करते थे। उनके बाद उनके शागिर्द अलक़मा (रहमतुल्लाह अलैह) ने वहाँ दर्स देना शुरू किया। उनके बाद उनके शागिर्द इबराहीम नख़ई (रहमतुल्लाह अलैह) वहाँ दर्स दिया करते थे, फिर इमाम साहब के उस्ताद हम्माद-बिन-अबी-सुलैमान ने वहाँ कई वर्षों तक दर्स दिया। उनके बाद हम्माद के शागिर्द इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) वहाँ दर्स दिया करते थे। यह बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद थी। लोगों ने इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) से दरख़ास्त की कि आप नमाज़ पढ़ाएँ। लोगों को जब पता चला कि इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) मिस्र से आए हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ाएँगे, तो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ख़ास तौर पर लोगों को शौक़ था कि ख़ुद इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) की ज़बान से क़िरअत सुनेंगे। चारों फ़ुक़हा में इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) एकमात्र फ़क़ीह हैं जिनका संबंध अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के ख़ानदान से है। इस वजह से भी लोगों को उनसे ख़ास अक़ीदत (श्रद्धा) थी। लेकिन लोगों की उम्मीदों के विपरीत इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) ने क़ुनूत नहीं पढ़ा। हालाँकि वह इसको अनिवार्य समझते थे। फ़ज्र की नमाज़ के बाद जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क़ुनूत क्यों नहीं पढ़ा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस साहबे-क़ब्र की राय के एहतिराम में नहीं पढ़ा। यह है इस्लाम और शरीअत का अस्ल स्वभाव।
एक और चीज़ जो दर्से-क़ुरआन के ग्रुपों को संगठित और संकलित करने में पेश आती है और जिसपर थोड़ी-सी चर्चा की ज़रूरत है वह पवित्र क़ुरआन का टेक्स्ट और अनुवाद है। याद रखें कि अरबी टेक्स्ट ही दरअस्ल क़ुरआन है। और जो अनुवाद है वह भी दरअस्ल टीका ही का एक अंग है। यानी एक अनुवादक ने अपनी समझ के अनुसार पवित्र क़ुरआन को समझा और उसका अनुवाद किया। पवित्र क़ुरआन के अनुवाद के लिए भी वे तमाम अपेक्षाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निभाने की ज़रूरत है जिनका मैंने तफ़सीर के अन्तर्गत उल्लेख किया था। तफ़सीर के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, वही पवित्र क़ुरआन के अनुवाद के लिए भी दरकार हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अरबी ज़बान नहीं जानता तो वह प्रत्यक्ष रूप से पवित्र क़ुरआन का अनुवाद नहीं कर सकता।
एक महत्त्वपूर्ण चीज़ यह है कि अगर दर्से-क़ुरआन से हमारा मक़सद दीन की दावत और शरीअत की शिक्षा है तो दोनों स्थितियों में पवित्र क़ुरआन से विद्यार्थी का लगाव पैदा करना अपरिहार्य है। जब तक पढ़नेवाले का प्रत्यक्ष जुड़ाव एवं लगाव पवित्र क़ुरआन के साथ न होगा उस वक़्त तक की कोशिश फलदायक साबित नहीं होगी। यह लगाव टेक्स्ट से होना चाहिए, अल्लाह की किताब के शब्दों से होना चाहिए। किसी अनुवादक या टीकाकार के अनुवाद से लगाव ज़रूरी नहीं। पवित्र क़ुरआन का अनुवाद सेवा के लिए है वह क़ुरआन की जगह नहीं ले सकता। अस्ल चीज़ पवित्र क़ुरआन का टेक्स्ट है जो चमत्कार है, अल्लाह के द्वारा अवतरित है, अर्थों और भावार्थों का समुद्र है।
अगर टेक्स्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाए और सारा ध्यान अनुवाद पर केन्द्रित कर दिया जाए तो मानो एक ओर तो हमने एक इंसान की समझ को पवित्र क़ुरआन के बराबर स्थान दे दिया, जो बहुत बड़ा दुस्साहस बल्कि अशिष्टता है। दूसरी ओर हमने क़ुरआन की व्यापकताओं को अनुवाद की संकीर्णताओं में सीमित कर डाला। कोई कितना ही बड़ा इंसान यहाँ तक कि उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) जैसा प्रतिष्ठित सहाबी क्यों न हो। उससे क़ुरआन के समझने में ग़लती हो सकती है और ग़लती से कोई मुक्त नहीं है।
एक बार की घटना है कि उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने महसूस किया कि लोगों ने मह्र मुक़र्रर करने में बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूख़र्ची से काम लेना शुरू कर दिया है, ऊँचे-ऊँचे मह्र मुक़र्रर किए जाने लगे हैं और ऊँचे मह्र मुक़र्रर करना बड़ाई का प्रतीक समझा जाने लगा है, तो उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर एलान किया कि आज के बाद मह्र की एक ख़ास मात्रा मुक़र्रर कर दी गई है और कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा मह्र न रखे। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इस मौक़े पर मौजूद थे। सबने इस फ़ैसले को सही क़रार दिया। नमाज़ के बाद जब उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ी महिला मिलीं और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से कहने लगीं कि तुमने जो मह्र की हद मुक़र्रर की है वह बिलकुल ग़लत है और तुम क़ुरआन को नहीं समझते। पवित्र क़ुरआन में तो आया है, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ अर्थात् “चाहे तुमने उनमें से किसी को ढेरों माल दे दिया हो, उसमें से कुछ वापस मत लेना।” (क़ुरआन, 4:20) यानी पवित्र क़ुरआन तो ढेर की संभावना को भी स्वीकार करता है। मानो दौलत का ढेर भी मह्र में दिया जा सकता है, अतः तुम कैसे कह सकते हो कि इस निर्धारित मह्र से ज़्यादा न दिया जाए।
उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक पल के लिए सोचा। वह ख़लीफ़ा राशिद (सदाचारी ख़लीफ़ा) थे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के उत्तराधिकारी थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उनकी मुबारक ज़बान से निकलनेवाले शब्दों की बार-बार ताकीद की थी। मैं सच कहता हूँ कि अगर उनकी जगह हमारे दौर का कोई मज़हबी लीडर, मौलवी या पीर होता तो आपत्ति करनेवाली महिला को डाँटकर चुप करा देता। लेकिन वह उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे, उन्होंने सब लोगों को दोबारा मस्जिद में वापस बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो वह मिंबर पर चढ़े और कहा, “उमर ने ग़लती की और एक औरत ने सच कहा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ।” यानी एक इतने बड़े इंसान से जो दीन का इतना बड़ा विद्वान है कि पवित्र क़ुरआन की 17 आयतें उसकी उम्मीद और अंदाज़े के अनुसार अवतरित हुईं, उससे भी क़ुरआन के समझने में ग़लती की संभावना है। पवित्र क़ुरआन में 17 स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहाँ उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अंदाज़ा किया कि दीन का स्वभाव यह अपेक्षा करता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए और उसी तरह हो गया। जब इस स्थान और रुतबे के आदमी से ग़लती हो सकती है और वह खुल्लम-खुल्ला उसको स्वीकार कर सकते हैं तो फिर और कौन किस गिनती में है।
दर्से-क़ुरआन में मौलिक चीज़ पवित्र क़ुरआन के शब्द और उनकी तिलावत (पाठ) है। यह बात मैंने इसलिए बताई कि कभी दर्से-क़ुरआन में टेक्स्ट की तिलावत करने के बजाय सिर्फ़ अनुवाद पढ़ने को काफ़ी समझ लिया जाता है। एक बार मैंने एक मशहूर मज़हबी व्यक्ति को देखा कि वह सिर्फ़ अनुवाद की मदद से दर्से-क़ुरआन दे रहे थे। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी और बहुत नागवार महसूस हुई कि अस्ल दर्स तो पवित्र क़ुरआन का देना अभीष्ट है। लेकिन अनुवाद को ही सब कुछ समझा जा रहा है। कम से कम पहले पवित्र क़ुरआन के शब्दों की तिलावत की जाए। लोगों को उसके शब्दों से परिचित करवाया जाए। और कोशिश की जाए कि लोग जिस हद तक समझ सकें उसको समझें और यह भी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
अगर आपके संबोधित उर्दू ज़बान अच्छी तरह जानते और समझते हैं तो उनके लिए बिना अरबी भाषा सीखे भी पवित्र क़ुरआन के आम अर्थ को कम से कम 50 प्रतिशत समझ लेना आसान है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पवित्र क़ुरआन के जितने भी शब्द आए हैं उनमें जो माद्दे (वह मूल अक्षर जिससे शब्द बनता है) इस्तेमाल हुए हैं, वे सारे के सारे 1500 के क़रीब हैं। उनमें 1400 से अधिक माद्दे वे हैं जो किसी न किसी रूप में उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ये 1400 माद्दे अगर पढ़नेवाले के ज़ेहन में रहें तो पवित्र क़ुरआन का आम अर्थ उसकी समझ में आ सकता है। और बार-बार अनुवाद पढ़ने और बार-बार दर्स सुनने से ख़ुद बख़ुद एक प्रवृत्ति और समझ पैदा हो जाती है।
मिसाल के तौर पर सूरा फ़ातिहा में हम्द, रब, आलमीन, रहमान, रहीम, मालिक, यौम, दीन इबादत, इस्तिआनत, हिदायत, सिराते-मुस्तक़ीम, इनाम, ग़ज़ब, ज़लाल। ये सब शब्द आम तौर पर उर्दू में प्रचलित हैं। इनमें से कोई शब्द भी ऐसा नहीं है जो उर्दू में इस्तेमाल न होता हो। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पवित्र क़ुरआन के अधिकतर शब्द किसी न किसी रूप में उर्दू ज़बान में प्रयुक्त होते हैं। अगर उन्हें नुमायाँ कर दिया जाए तो पढ़नेवाला बड़ी आसानी से पवित्र क़ुरआन के मतलब तक पहुँच सकता है।
तीसरी चीज़ यह है कि पवित्र क़ुरआन का अनुवाद जितने लोगों ने भी किया है ज़ाहिर है कि बहुत निष्ठापूर्वक और दर्दमंदी के साथ किया है, और कोशिश की है कि पवित्र क़ुरआन के सन्देश को आम इंसानों तक पहुँचाया जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि पवित्र क़ुरआन का अनुवाद इस तरह करना कि अल्लाह की किताब में जो कुछ कहा गया है, वह ज्यों का त्यों पढ़नेवाले तक स्थानांतरित हो जाए, यह संभव नहीं है। न केवल उर्दू बल्कि किसी भी भाषा में ऐसा कर दिखाना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि पवित्र क़ुरआन ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उन शब्दों में अर्थों का इतना असीम समुद्र छिपा हुआ है कि पवित्र क़ुरआन के शब्दों का विकल्प दुनिया की किसी भाषा में मिल ही नहीं सकता। किसी भी और शब्द में वह सारगर्भिता मौजूद नहीं है जो पवित्र क़ुरआन के शब्दों में है। इसलिए मात्र अनुवाद को पर्याप्त समझना पवित्र क़ुरआन के सन्देश को अधूरे तौर पर पहुँचाने के समान है। जब तक अस्ल शब्दों से संबंध क़ायम न हो पवित्र क़ुरआन की रूह तक पहुँच संभव नहीं।
कभी-कभी पवित्र क़ुरआन का अनुवाद करने में कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने तो जान-बूझकर उन मामलों का ध्यान नहीं रखा, और कुछ लोगों ने ध्यान रखना चाहा तो इसकी सीमाएँ उनसे क़ायम न रह सकीं। इसमें किसी बदनीयती का कोई दख़ल नहीं है, बल्कि पवित्र क़ुरआन के शब्दों की सारगर्भिता और अर्थों की व्यापकता के अलावा पवित्र क़ुरआन की शैली अपने अंदर वह निरालापन रखती है जिसको किसी और भाषा में स्थानांतरित ही नहीं किया जा सकता।
जैसा कि मैंने आरंभ ही में कह दिया था कि पवित्र क़ुरआन की शैली संबोधन और भाषण की है, संबोधन और भाषण की शैली में बहुत-सी चीज़ें छिपी होती हैं। उनके अलावा कुछ छिपी चीज़ें अरबी भाषा की शैली की दृष्टि से होती हैं। अब जब एक व्यक्ति पवित्र क़ुरआन का अनुवाद करता है, उदाहरणार्थ शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। उन्होंने अपनी असाधारण परहेज़गारी की वजह से यह काम किया कि पवित्र क़ुरआन के शब्दों का उर्दू में अनुवाद ज्यों का त्यों कर दिया, यानी हर शब्द का अनुवाद उसके नीचे लिख दिया। जैसे ‘साथ नाम अल्लाह के जो रहमान है, रहीम है।’ यानी कोशिश यह की कि अनुवाद में कोई शब्द अस्ल से आगे पीछे न होने पाए, और पवित्र क़ुरआन के अर्थ में किसी निजी राय का कण बराबर हस्तक्षेप न होने पाए। सावधानी और परहेज़गारी की दृष्टि से तो निस्सन्देह यह बहुत ऊँची बात है। लेकिन इससे क़ुरआन का सन्देश पहुँचाने का वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जो दर्से-क़ुरआन का होता है।
शाह रफ़ीउद्दीन के ज़माने के बाद इस अंदाज़ के अनुवाद बहुत अधिक आए तो लोगों ने महसूस किया कि इससे वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा जो उन अनुवादों के सामने था। महसूस यह किया गया कि पवित्र क़ुरआन को इस तरह की भाषा में बयान करना चाहिए कि आम आदमी उसको अपने दिल के अंदर उतरता हुआ महसूस करे। चुनाँचे इस एहसास को देखते हुए शाब्दिक अनुवाद के बजाय पवित्र क़ुरआन के बा-मुहावरा अर्थात् प्रवाहित शैली में अनुवाद का रिवाज शुरू हो गया।
मुहावरेदार अनुवाद के ध्वजावाहक बुज़ुर्गों में से एक गिरोह ने यह उचित समझा कि जिस भाषा का जो मुहावरा है उसके हिसाब से अनुवाद होना चाहिए। इन लोगों में शायद सबसे नुमायाँ नाम मिर्ज़ा हैरत देहलवी और मौलवी नज़ीर अहमद के हैं। मौलवी नज़ीर अहमद, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मशहूर हैं, दिल्ली के रहनेवाले थे, उर्दू भाषा के पहली पंक्ति के साहित्यकारों में गिने जाते थे। बल्कि उर्दू भाषा के जो चार स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक थे। उन्होंने पवित्र क़ुरआन का मुहावरेदार भाषा में अनुवाद किया, इसलिए दिल्ली के मुहावरे की भाषा अपनाई।
इसपर कुछ सावधान प्रवृत्ति के विद्वानों को ख़याल हुआ कि मुहावरे की पाबंदी की यह कोशिश हद से बाहर चली गई है और गोया उर्दू भाषा की ज़रूरत को पवित्र क़ुरआन के शब्दों और शैली पर वरीयता प्राप्त हो गई है। ऐसा महसूस हुआ कि किसी-किसी जगह उन्होंने पवित्र क़ुरआन के शब्दों को नज़र अंदाज़ कर दिया है। उदाहरणार्थ उन्होंने ‘ज़ुख़रुफ़ुल-क़ौल’ का अनुवाद किया है ‘चिकनी-चुपड़ी बातें’। अब ज़ुख़रुफ़ का अर्थ है लेप की हुई चीज़, बनाई-सँवारी हुई बात। अभिप्रेत यह है कि विधर्मी बातों को इस क़दर ख़ूबसूरत बनाकर पेश करते हैं कि लोग उनकी तरफ़ उन्मुख हों। अब इसका शाब्दिक अनुवाद चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं है। चिकनी-चुपड़ी बातों से हो सकता है कि यह अर्थ की हद तक अदा हो जाए, लेकिन ज़ुख़रुफ़ का अर्थ न चिकने के हैं और न चुपड़े के। सावधान प्रवृत्ति के बुज़ुर्गों का ख़याल था कि अनुवाद सही नहीं है। इसलिए कि यह क़ुरआन की भाषा का सीमोल्लंघन है।
अगर क़ुरआन की भाषा के अंदर रहकर मुहावरे की पाबंदी की जाए तो फिर ठीक है। कोशिश यह की जाए क़ुरआन की भाषा की भी पाबंदी हो और ज़बान का मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती है कि पवित्र क़ुरआन के शब्दों और भाषा के अंदर रहकर उर्दू मुहावरे का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल काम है। मुहावरा पवित्र क़ुरआन के चौखटे से निकल-निकल पड़ता है। कुछ दूसरे विद्वानों ने इसका एक और हल निकाला। इन बुज़ुर्गों ने यह शैली अपनाई कि जहाँ ज़रूरत पेश आए वहाँ कोष्ठक लगा दिया जाए और वहाँ स्पष्ट कर दिया जाए, पवित्र क़ुरआन के शब्द तो अनुवाद में ज्यों के त्यों बरक़रार रहें और जिन शब्दों की वृद्धि करना अभीष्ट हो उनको कोष्ठक में दे दिया जाए। लेकिन इससे अनुवाद में एक कमज़ोरी यह पैदा होती है कि वह विद्यार्थी और विद्वान जो अरबी भाषा की शैली से स्वयं अवगत नहीं हैं और सिर्फ़ अनुवाद पढ़ते हैं, उनके लिए कभी-कभी यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कोष्ठक में जो चीज़ आई है, वह कहाँ अनुवादक की अपनी समझ है और कहाँ पवित्र क़ुरआन के छिपे हुए शब्दों को ज़ाहिर किया गया है और कहाँ वह वृद्धि किसी हदीस या असर से ली गई है। अब या तो कोष्ठक में बयान की हुई इन सब चीज़ों को एक सतह पर रखकर उसी तरह प्रमाणित मान लिया जाए जिस तरह पवित्र क़ुरआन के अपनी छिपे शब्द हैं। या उन सबको मुफ़स्सिर (टीकाकार) की व्याख्या समझकर क़ुरआन के टेक्स्ट से बाहर की चीज़ क़रार दिया जाए। इसका नतीजा यह निकलेगा कि बहुत-सी महत्त्वपूर्ण चीज़ें महत्त्वहीन हो जाएँगी।
इसपर कुछ लोगों ने कहा कि पवित्र क़ुरआन के अनुवाद में कोष्ठक नहीं होने चाहिएँ। कुछ लोगों ने यह शैली निकाली कि हर शब्द पर एक फ़ुटनोट दे दिया जाए और वहाँ अस्ल अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाए। यह भी एक अच्छा तरीक़ा है लेकिन फ़ुटनोट में पढ़नेवाले पाठकों को बड़ी दिक़्क़त पेश आती है। आप अनुवाद प्रवाहित और लगातार शैली में पढ़ना चाहते हैं, दरमियान में हर लफ़्ज़ पर फ़ुटनोट आ रहा है, इससे आपका ध्यान हट जाता है। प्रवाह और निरन्तरता हाथ से निकल जाती है।
अनुवाद की एक और शक्ल पवित्र क़ुरआन में ‘ज़माइर’ (सर्वनामों) का अनुवाद है। अरबी भाषा में ‘तसनिया’ (द्विवचन) का सर्वनाम और है ‘जमा’ (बहुवचन) का और है। ‘मुअन्नस’ (स्त्रीलिंग) की ज़मीर (सर्वनाम) और है और ‘मुज़क्कर’ (पुल्लिंग) की और। उर्दू (और हिन्दी) में द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम एक हैं। पवित्र क़ुरआन में तो ‘ज़मीर’ (सर्वनाम) से अंदाज़ा हो जाएगा कि यह इशारा किस तरफ़ है। कुछ लोगों ने इसका हल यह निकाला कि जहाँ सर्वनाम है वहाँ सर्वनाम के बजाय उस शब्द को ही बयान कर दिया जाए। लेकिन जहाँ एक सर्वनाम का संबंध एक से अधिक से जुड़ रहा हो वहाँ अनुवादक को अपनी समझ के अनुसार किसी एक को निर्धारित करना पड़ेगा। जब वह अपनी समझ के लिहाज़ से संबंधित का निर्धारण करके अनुवाद करेगा तो वह अनुवाद, अनुवाद नहीं रहेगा बल्कि टीका हो जाएगी। ये वे बारीकियाँ हैं जो पवित्र क़ुरआन के अनुवाद में ध्यान में रखनी चाहिएँ।
इस बात के स्पष्टीकरण के लिए मैं यहाँ डिप्टी नज़ीर अहमद के अनुवाद की मिसाल देता हूँ पवित्र क़ुरआन में आया है, لِکُلِّ امۡرِیًٔ مِّنۡہُمۡ یَوۡمَئِذٍ شَاۡنٌ یُّغۡنِیۡ, यानी “उनमें से हर व्यक्ति की उस दिन एक ख़ास हालत होगी जो उसे दूसरों से उदासीन कर देगी।” इस आयत का शाब्दिक अर्थ तो यह हुआ। अब मुहावरेदार अनुवाद के ध्वजावाहक एक महाशय ने तो इसका अनुवाद यह किया कि इस दिन हर व्यक्ति को अपनी-अपनी पड़ी होगी। इससे अर्थ स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन इस अनुवाद में पवित्र क़ुरआन के किसी एक शब्द का भी शाब्दिक अनुवाद नहीं आया। क्या इस तरह का अनुवाद होना चाहिए? कुछ सावधान प्रवृत्ति के बुज़ुर्गों की राय है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी राय में यह बिल्कुल नाजायज़ है। कुछ लोगों का ख़याल है ऐसा अनुवाद करने में कोई हरज नहीं। इसलिए कि चाहे शाब्दिक अनुवाद न हो, लेकिन इससे अर्थ तो स्थानांतरित हो जाएगा। और अगर पढ़नेवाला उर्दू भाषा का स्वभाव जानता है तो यक़ीनन इससे असर लेगा। तीसरी राय यह है कि अनुवाद तो शाब्दिक हो लेकिन अर्थ का ज़रूरी विवरण फ़ुटनोट में बयान कर दिया जाए। एक और बुज़ुर्ग ने उपर्युक्त आयत का अनुवाद किया कि “उस रोज़ हर व्यक्ति अपने-अपने हाल में मगन होगा।” इससे भी आयत की मुराद बड़ी हद तक समझ में आ जाती है। लेकिन शाब्दिक अनुवाद यह भी नहीं है।
जहाँ तक पवित्र क़ुरआन के अनुवाद का संबंध है, इसकी चार शक्लें या चार सतहें संभव हैं, और सच्ची बात यह है कि पवित्र क़ुरआन को समझने या समझाने के लिए वे चारों शक्लें ज़रूरी हैं। आज उर्दू के जितने अनुवाद भी उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या लगभग साढ़े तीन सौ है, वे उन्ही चारों में से किसी न किसी सतह की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अनुवाद की एक सतह तो ‘तहतल्लफ़्ज़’ (शब्द के नीचे अनुवाद) और शाब्दिक अनुवाद की है। यानी पवित्र क़ुरआन के एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द रख दिया जाए, जैसा कि शाह रफ़ीउद्दीन के अनुवाद की मिसाल में बयान हुआ, बड़ी हद तक शैख़ुल-हिंद मौलाना महमूद हसन का अनुवाद भी शाब्दिक ही है। इन अनुवादों में अरबी शब्द के नीचे इसका उर्दू समानार्थी शब्द लिख दिया गया है।
लेकिन कुछ जगह उर्दू समानार्थी शब्दों से काम नहीं चलता। उदाहरणार्थ किसी जगह अरबी शब्द के तीन या चार अर्थ निकलते हैं और अनुवादक ने अनुवाद में उर्दू का एक ही समानार्थी शब्द लिख दिया है तो ऐसा करने से पवित्र क़ुरआन के अर्थ सीमित हो जाते हैं। शाब्दिक अनुवाद की यह मौलिक कमजोरी है। लेकिन अत्यंत सावधानी और सुरक्षित रास्ता है कि पवित्र क़ुरआन में कम से कम अपनी राय से कोई बात न कही जाए। अगरचे किसी हद तक राय उसमें भी आ जाती है।
दूसरी शैली यह है कि पवित्र क़ुरआन का अनुवाद करते समय व्याकरण संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाए। व्याकरण की अपेक्षा से मुराद यह है कि वाक्य की बनावट और विधि में अनुवाद की भाषा का ध्यान रखा जाए। अरबी भाषा में वाक्य का क्रम और है और उर्दू में क्रम और है। अरबी भाषा में वाक्य ‘फ़ेअल’ (कर्म) से शुरू होता है। ‘ज़-र-ब ज़ैदु उमरा’। उर्दू (और हिन्दी) में वाक्य ‘फ़ाइल’ (कर्ता) से शुरू होता, ‘फ़ेअल’ आख़िर में आता है। अब कुछ लोगों ने यह किया कि अनुवाद अलग-अलग शब्दों और वाक्यों की हद तक तो शाब्दिक हो मगर व्याकरण के क्रम की दृष्टि से उर्दू की शैली की पैरवी की जाए। और वाक्य को इस क्रम से रखा जाए जिस क्रम से उर्दू भाषा में वाक्य आते हैं। ज़ाहिर है कि यह क्रम पवित्र क़ुरआन के क्रम से विभिन्न होगा जो उर्दू में प्रचलित नहीं है। यह मानो व्याकरण के अनुसार अनुवाद होगा।
अनुवाद का एक और प्रकार या सतह जिसको हम शैलीगत अनुवाद कह सकते हैं, यह है कि पवित्र क़ुरआन की शैली को अपनाकर उर्दू में बयान करने की कोशिश की जाए और लोग पवित्र क़ुरआन की शैली से परिचित हो जाएँ और उन्हें वह अनुवाद असहज न लगे।
एक सतह अनुवाद की वह है कि जिसको मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) तरजुमानी (प्रवक्तव्य) कहते हैं। पवित्र क़ुरआन की एक आयत को लेकर इस अंदाज़ से उसकी तरजुमानी की जाए कि न तो वह शाब्दिक अनुवाद हो और न ही मुहावरेदार अनुवाद हो, बल्कि उसे अनुवाद कहा ही न जाए और तरजुमानी का नाम दिया जाए। इसमें थोड़ी-सी आज़ादी अनुवादक को मिल जाती है कि वह एक वाक्य का अर्थ कई वाक्यों में बयान कर देता है। मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने तफ़हीमुल-क़ुरआन में पवित्र क़ुरआन की तरजुमानी की है, अनुवाद नहीं किया, इसलिए पढ़नेवालों को भी यह समझकर पढ़ना चाहिए कि यह पवित्र क़ुरआन का अनुवाद नहीं है, बल्कि उसके अर्थ का स्पष्टीकरण है।
एक आम सवाल जो पवित्र क़ुरआन के बहुत-से नौ-सिखिए विद्यार्थी करते हैं, यह है कि पवित्र क़ुरआन के अनगिनत अनुवाद और टीकाओं में से किसको बुनियाद बनाया जाए और दर्स देते वक़्त किसको सामने रखा जाए। सच्ची बात यह है कि जिन लोगों ने भी पवित्र क़ुरआन के अनुवाद और टीका का काम किया है वे अत्यंत असाधारण लोग थे। कोई साधारण लोग नहीं थे, उन्होंने अत्यंत निष्ठा के साथ आधी-आधी सदी पवित्र क़ुरआन के अध्ययन में गुज़ारी, उसके बाद यह अज़ीमुश्शान काम अंजाम दिया। लेकिन इन सब प्रयासों के अत्यंत सम्मान के बावजूद ये सारे प्रयास एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की क़ुरआन की समझ को बयान करते हैं।
तफ़हीमुल-क़ुरआन का दर्जा आधुनिक टीका संबंधी साहित्य में बहुत ऊँचा है। लेकिन बहरहाल वह मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) की क़ुरआन की समझ है। तदब्बुर क़ुरआन बहुत ऊँची टीका है, लेकिन वह मौलाना इस्लाही (रहमतुल्लाह अलैह) और मौला फ़राही (रहमतुल्लाह अलैह) की समझ और अन्तर्दृष्टि पर आधारित है। मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रहमतुल्लाह अलैह) की बयानुल-क़ुरआन और मौलाना मुफ़्ती शफ़ी (रहमतुल्लाह अलैह) की मआरिफ़ुल-क़ुरआन बड़ी उच्च कोटि की टीकाएँ हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना थानवी और मुफ़्ती शफ़ी की समझ पर आधारित हैं। उनमें से कोई प्रयास भी ख़ुद क़ुरआन का स्थानापन्न नहीं हो सकता।
अगर ग़लती अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से हो सकती है तो फिर कोई व्यक्ति भी ग़लती से मुक्त नहीं है। उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से क़ुरआन समझने में चूक होती है और वह उसको मुखर रूप से स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ आजकल यह कहना तो बहुत आसान है कि उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से ग़लती हो गई, हमारे लिए यह कह देना भी बहुत सरल है कि इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) ने अमुक जगह ग़लती की और यह कह देना भी बहुत आसान है कि इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) ने अमुक बात सही नहीं कही। हमारी दीनी दर्सगाहों में रोज़ ये आलोचनात्मक टिप्पणियाँ होती रहती हैं, लेकिन यह कहने की किसी की मजाल नहीं है कि मौलाना थानवी या मौलाना मौदूदी या मौलाना अहमद रज़ा ख़ान से ग़लती हुई। कोई ज़रा यह जुरअत करके देखे। उनके मुरीद सर तोड़ देंगे। और इस्लाम से ख़ारिज करके दम लेंगे। [मौलाना मौदूदी के ‘मुरीदों’ के संबंध में लेखक की यह राय दुरुस्त नहीं है। सच तो यह है जमाअत इस्लामी अपनी तमाम व्यावहारिक कमज़ोरियों के बावजूद मस्लक परस्ती और शख़्सियत परस्ती या अंधभक्ति जैसी बुराइयों से अब भी मुक्त है।...........अनुवादक]
लेकिन उनमें से हर अनुवाद में कुछ विशेषताएँ हैं जो दूसरे अनुवादों में नहीं हैं। इसलिए बेहतर और सुरक्षित रास्ता यह है कि बजाय एक अनुवाद को बुनियाद बनाने के एक से अधिक अनुवादों को आधार बनाया जाए। एक शाब्दिक अनुवाद ले लें, एक मुहावरेदार अनुवाद ले लें और एक तरजुमानी का नमूना ले लें। इन सबको सामने रखकर दर्से-क़ुरआन की तैयारी करें, ताकि जहाँ तक संभव हो ग़लती से बच सकें, जो इस आयत का बेहतरीन अर्थ है जिसे तीन बड़े टीकाकारों ने बयान किया हो इस तरह अध्ययन करने से इस आयत का सार सामने आ जाएगा।
इन अनुवादकों में से हर एक को इन मुश्किलों का अंदाज़ था, जो अनुवाद करते समय सामने आती हैं। कौन इस मुश्किल से किस तरह निकला? यह ख़ुद अपनी जगह एक ज्ञानपरक काम है और इससे रास्ता आसान हो जाता है। यही मामला तफ़सीर का है कि पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर (टीका) इन बुज़ुर्गों में से हर एक ने एक ख़ास ज़रूरत को सामने रख कर की है। उदाहरणार्थ मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) ने लिखा है कि उनके समाने इस्लामी ज्ञान के विद्यार्थी या इस्लामी विद्वान नहीं हैं। बल्कि उनके सामने आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग है जो पवित्र क़ुरआन को समझना चाहता है। यह वर्ग मुश्किलातुल-क़ुरआन और बड़े-बड़े कलात्मक मामलों में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि पवित्र क़ुरआन के सन्देश को सीधी-साधी ज़बान में सीखना और समझना चाहता है। मौलाना मौदूदी (रहमतुल्लाह अलैह) का कहना है कि तफ़सीर मैं इस वर्ग के लिए लिख रहा हूँ। अब यह निर्धारित हो गया कि मौलाना के संबोधित कौन लोग हैं।
डिप्टी नज़ीर अहमद ने जब पवित्र क़ुरआन का अनुवाद किया तो उन्होंने कहा कि मैं पवित्र क़ुरआन को उस उर्दू भाषी वर्ग तक पहुँचाना चाहता हूँ जो उर्दू की प्रवृत्ति रखता है, और उर्दूगा मुहावरे के द्वारा ज़्यादा आसानी से पवित्र क़ुरआन को समझ सकता है। यों उनके संबोधित भी निर्धारित हो गए। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही (रहमतुल्लाह अलैह) ने लिखा है कि मैं तफ़सीर उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो अरबी साहित्य की प्रवृत्ति रखते हैं और अरबी भाषा की सुन्दरता और उत्कृष्टता एवं वाग्मिता को भी समझना चाहते हैं। उनके संबोधित भी निर्धारित हो गए।
अब अगर मेरे सामने दर्स देते समय तफ़हीमुल-क़ुरआन और तदब्बुर क़ुरआन दोनों हों तो मेरे सामने तफ़सीर की दो शैलियाँ और क़ुरआन समझने की दो प्रवृत्तियाँ आ गईं। उलूमे-क़ुरआन और मुश्किलाते-क़ुरआन में 99 प्रतिशत पर तो ये दोनों टीकाकार पूरे तौर पर सहमत होंगे। जहाँ उनमें मतभेद होगा उससे कम से कम मुझे इतना मालूम हो जाएगा कि यहाँ पवित्र क़ुरआन की व्याख्या में एक से अधिक मतलब संभव हैं। अब अगर मुझे शौक़ होगा तो मैं और तफ़सीरें देख लूँगा और मेरे सामने एक स्पष्ट रूप आ जाएगा। इसलिए क़ुरआन की तफ़सीर में भी एक से अधिक तफ़सीरों को सामने रखना न केवल मुनासिब, बल्कि ज़रूरी है। जिन विद्वानों से आपकी प्रवृत्ति मिलती हो, और जिनके इल्म और तक़्वा और दीन की समझ पर आपको भरोसा हो, उन्ही में से तीन बुज़ुर्गों की तफ़ासीर ले लीजिए। कोई से तीन अनुवाद और कोई सी तफ़सीरें आप मुंतख़ब कर लें और उनको बुनियाद बनाकर आप दर्से-क़ुरआन की तैयारी शुरू कर दें।
एक आख़िरी सवाल यह पैदा होता है कि कोई-सी तीन तफ़सीरें अगर चुनी जाएँ तो आख़िर कौन-सी चुनी जाएँ। यहाँ आपको अपने संबोधितों को सामने रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके संबोधित आला दर्जे के शिक्षित लोग हैं। अगर ऐसा है तो फिर वह इस प्रकार के मामले नहीं उठाएँगे जो पुरानी तफ़सीरों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ इशाइरा, मातुरीदिया और मोतज़िला के मसाइल न वे जानते हैं और न उनसे दिलचस्पी ही रखते हैं। अतः वे तफ़सीरें आपके दायरे से ख़ारिज हो गईं जिनमें इस प्रकार की बहसें आई हैं। यहाँ वह तफ़सीरें ज़्यादा प्रभावकारी होंगी जो आधुनिक पश्चिमी चिन्तकों की आपत्तियों और सन्देहों का जवाब देती हैं। उदाहरणार्थ मौलाना अब्दुल-माजिद दरियाबादी (रहमतुल्लाह अलैह) की तफ़सीरे-माजिदी।
अगर आपके विद्यार्थियों में अरबी की प्रवृत्ति रखनेवाले हैं तो फिर आप मौलाना इस्लाही की तफ़सीर ले लें। इस तरह अगर आपके संबोधितों की सतह और उनकी प्रवृत्ति देखकर तफ़सीर का चयन करें तो उनके लिए ज़्यादा आसान और लाभप्रद होगा। इसलिए कि अगर उद्देश्य दीन और शरीअत की शिक्षा है तो फिर संबोधित की ज़रूरत का ध्यान रखना सुन्नते-नबवी में शामिल है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का तरीक़ा था कि सवाल करनेवाले की सतह और पृष्ठभूमि के अनुसार जवाब दिया करते थे। बहुत-से लोगों ने विभिन्न अवसरों पर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से सवाल किया कि बेहतरीन देश कौन-सा है तो आपने विभिन्न जवाब दिए और हर एक की ज़रूरत को सामने रखा।
अपने संबोधितों में पवित्र क़ुरआन के टेक्स्ट से लगाव पैदा करने की कोशिश करें। यह काम उस वक़्त ज़्यादा आसानी से हो सकता है जब संबोधितगण और विद्यार्थी पवित्र क़ुरआन के अधिकतर हिस्से के हाफ़िज़ और उसके शब्दों से अच्छी तरह परिचित हों। आजकल यह काम बहुत आसान हो गया है। बड़े-बड़े क़ारियों के कैसेट मौजूद हैं। श्रवण शक्ति से काम लें, बार-बार सुनने से लहजा भी दुरुस्त हो जाएगा और बहुत-सा हिस्सा पवित्र क़ुरआन का हिफ़्ज़ (कंठस्थ) भी हो जाएगा। बहुत आसानी की बात मैंने इसलिए की है कि आजकल हमारे यहाँ हिफ़्ज़ के माहिरों की एक सऊदी टीम आई है, जिसने कोई ख़ास तकनीक ईजाद की है कि वे एक महीने में बच्चे को पूरा पवित्र क़ुरआन हिफ़्ज़ करवा देते हैं। ज़ाहिर है कि वह तमाम आधुनिक मशीनरी इस्तेमाल करते होंगे। और बचचे की भी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल की जाती होंगी। इससे ज़रूर अंदाज़ा हुआ कि आधुनिक संसाधनों से काम लेकर पवित्र क़ुरआन को बहुत अच्छी तरह सीखा और पढ़ा जा सकता है।
(Follow/Subscribe Facebook: HindiIslam,Twitter: HindiIslam1, YouTube: HindiIslamTv, E-Mail: HindiIslamMail@gmail.com)
Recent posts
-

क़ुरआन मजीद का परिचय
29 April 2024 -

क़ुरआन की शिक्षाएँ मानवजाति के लिए अनमोल उपहार
27 March 2024 -
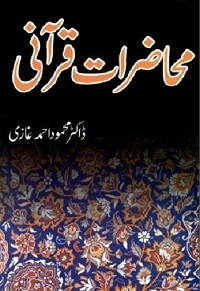
पवित्र क़ुरआन का विषय और महत्त्वपूर्ण वार्त्ताएँ (क़ुरआन लेक्चर - 11)
12 December 2023 -
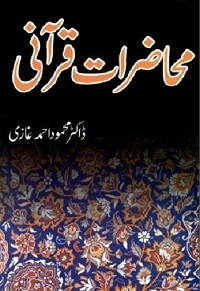
नज़्मे-क़ुरआन और क़ुरआन की शैली (क़ुरआन लेक्चर- 10)
12 December 2023 -
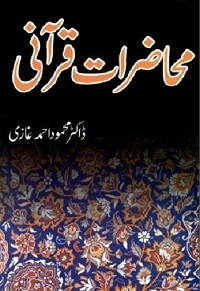
उलूमुल-क़ुरआन-क़ुरआन से संबंधित ज्ञान (क़ुरआन लेक्चर - 9)
12 December 2023 -
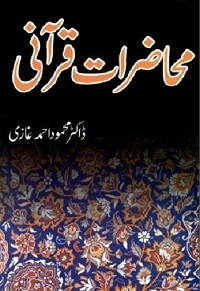
क़ुरआन के चमत्कारी गुण (क़ुरआन लेक्चर - 8)
12 December 2023

