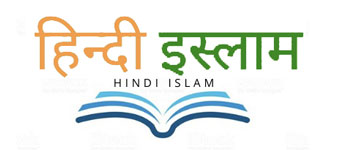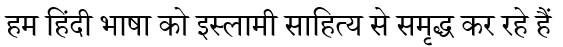क़ुरआन के टीकाकारों की टीका-शैलियाँ (क़ुरआन लेक्चर - 7)
-
कु़रआन (लेख)
- at 12 December 2023
क़ुरआन प्रबोधन - 7: क़ुरआन के टीकाकारों की टीका-शैलियाँ
डॉ० महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक: गुलज़ार सहराई
लेक्चर नम्बर-7 (14 अप्रैल 2003)
[क़ुरआन से संबंधित ये ख़ुतबात (अभिभाषण), “मुहाज़राते-क़ुरआनी” जिनकी संख्या 12 है, इनमें पवित्र क़ुरआन, उसके संकलन के इतिहास और उलूमे-क़ुरआन (क़ुरआन संबंधी विद्याओं) के कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें यह बताया गया है कि क़ुरआन को समझने और उसकी व्याख्या करने की अपेक्षाएँ क्या हैं, उनके लिए हदीसों और अरबी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ अरबों के इतिहास और प्राचीन अरब साहित्य की जानकारी भी क्यों ज़रूरी है और इस जानकारी के अभाव में क़ुरआन के अर्थों को समझने में क्या-क्या समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। ये अभिभाषण क़ुरआन के शोधकर्ताओं और उसे समझने के इच्छुक पाठकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।]
टीका-शैलियों से अभिप्रेत वह ढंग और विधि है जिसके अनुसार किसी टीकाकार ने पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर या टीका की हो, या उस कार्य-विधि के अनुसार पवित्र क़ुरआन की टीका को संकलित करने का इरादा किया है। हम सब का ईमान (विश्वास) है कि पवित्र क़ुरआन रहती दुनिया तक के लिए है, और दुनिया के हर इंसान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। इस अस्थायी सांसारिक जीवन में इंसानों को अच्छा इंसान बनाने में जिन-जिन पहलुओं के बारे में कल्पना की जा सकती है, उन सब के बारे में पवित्र क़ुरआन मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। पवित्र क़ुरआन एक व्यापारी के लिए भी मार्गदर्शक किताब है, एक शिक्षक के लिए भी मार्गदर्शक किताब है, एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री और क़ानून-विशेषज्ञ के लिए भी मौलिक सिद्धांत उपलब्ध करता है। कहने का तात्पर्य यह कि ज़िंदगी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसका संबंध इंसान को बेहतर इंसान बनाने से हो और उसके बारे में पवित्र क़ुरआन मार्गदर्शन न उपलब्ध करता हो।
चुनाँचे यह बात बजा तौर पर बिल्कुल सही और बिल्कुल वास्तविकता के अनुसार थी कि पिछली चौदह सदियों के दौरान में विभिन्न प्रवृत्तियाँ रखनेवाले विद्वान, और विभिन्न वैचारिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले विद्वान अपनी-अपनी आवश्यकताओं और अपनी-अपनी अपेक्षाओं के अनुसार पवित्र क़ुरआन की ओर उन्मुख हुए और पवित्र क़ुरआन से मार्गदर्शन प्राप्त किया। फिर उन्होंने इस मार्गदर्शन को अपने समविचार, समरुचि और अपने जैसी आवश्यकता रखनेवाले लोगों तक पहुँचाने का प्रबंध किया।
पर चूँकि पवित्र क़ुरआन अरबी भाषा में है, बल्कि स्पष्ट अरबी में है, और अरबी भी वह जो उत्कृष्टता एवं वाग्मिता की उच्चकोटि के शिखर पर है। इसलिए पवित्र क़ुरआन की उत्कृष्टता एवं वाग्मिता और अरबीयत का अध्ययन भी विद्वानों की दिलचस्पी का केन्द्र रहा है, (इस ओर इससे पहले एक अभिभाषण में इशारा किया जा चुका है) चुनाँचे बहुत जल्द जहाँ दूसरे ज्ञान-विज्ञान में विशिष्टता आरंभ हुई वहाँ पवित्र क़ुरआन के ज्ञान-विज्ञान में भी विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार विशिष्टता की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस पूरी प्रक्रिया का आधार प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के तफ़सीरी (टीका संबंधी) दर्सों और उनसे उल्लिखित तफ़सीरी रिवायतें हैं।
जैसा कि पहले कई बार बताया गया, जिन प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से तफ़सीरी रिवायतें उल्लिखित हैं या जिनके तफ़सीरी इज्तिहादात (निजी रायों) का बाद के तफ़सीरी साहित्य पर गहरा प्रभाव है, उनमें सबसे नुमायाँ प्रतिष्ठित सहाबा दो हैं। अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु)। इन दोनों बुज़ुर्गों की तफ़सीरी रिवायतों में वे तमाम मूल तत्त्व पहले दिन ही से स्पष्ट रूप से से होते हैं जिनके अनुसार बाद में तफ़सीरें लिखी जाती रहीं। यह दोनों लोग प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में अपनी सुरुचि की दृष्टि से, अरबी भाषा में अपनी निपुणता की दृष्टि से, असाधारण भाषण कला की और वाग्मिता के दृष्टि से. अपनी फ़क़ीहाना बसीरत (धर्मशास्त्रीय अन्तर्दृष्टि) की दृष्टि से, और इन सब चीज़ों के साथ-साथ अपनी असाधारण परिपक्व सोच, असाधारण उदारता और असाधारण वैचारिक गहनता में बहुत नुमायाँ और विशिष्ट स्थान रखते थे। यह बात इसलिए याद रखनी ज़रूरी है कि पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर की जितनी प्रवृत्तियाँ और शैलियाँ विभिन्न समयों में सामने आई हैं उनमें से किसी शैली के बारे में यह कल्पना करना सही न होगा कि वह प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से उल्लिखित इन रिवायतों की क्रमबद्धता से बिलकुल हटकर कोई नई चीज़ है, बल्कि सच तो यह है कि इन सरी प्रवृत्तियों की सनद प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के कथनों से मिलती है। इन सब शैलियों की बुनियादें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से उल्लिखित रिवायतों और उन इज्तिहादात (मतों) में मौजूद हैं, जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने पवित्र क़ुरआन के बारे में किए। और ख़ास तौर पर उन दो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के तफ़सीरी कथन और रायों में वे सारे तत्त्व मौजूद हैं जिनसे बड़ी संख्या में ताबिईन ने लाभ उठाया। उनमें से अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनके कुछ मशहूर शिष्यों का उल्लेख किया जा चुका है। अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उनकी टीका संबंधी प्रवृत्तियों के बारे में भी इशारा किया जा चुका है। उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है। जिनसे ख़ास तौर पर कूफ़ा और मदीना मुनव्वरा में तफ़सीरी रिवायतें आम हुईं।
यह निर्धारण तो निश्चित रूप से करना संभव नहीं है कि पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर में कुल कित्तनी प्रवृत्तियाँ पैदा हुईं। इसलिए कि जब तक इंसानी ज़ेहन काम करता रहेगा, नई-नई प्रवृत्तियाँ पैदा होती रहेंगी। चुनाँचे ख़ुद बीसवीं सदी ईस्वी में कई नई प्रवृत्तियाँ सामने आईं जिनका आगे चलकर उल्लेख किया जाएगा। जब तक इंसान इस धरती पर मौजूद है और पवित्र क़ुरआन के मानने वाले मौजूद हैं, वे पवित्र क़ुरआन के नए-नए अर्थों पर विचार करते रहेंगे और यों इल्मे-तफ़सीर (क़ुरआन का टीका-ज्ञान) की नई-नई शैलियोँ, नए-नए तरीक़े और नई- नई प्रवृत्तियाँ सामने आती रहेंगी।
क़ुरआन के अध्ययन का एक विशेष आयाम और इससे संबंधित एक दिलचस्प घटना जो अभी-अभी मेरे ज़ेहन में आई है, मैं पहले उसका ज़िक्र कर देता हूँ। इस दिलचस्प घटना का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पवित्र क़ुरआन के अध्यन के अभी इतने अछूते मैदान मौजूद हैं जो अभी तक विचाराधीन भी नहीं लाए गए। क़ुरआन की टीका के तो इतने अथाह समुद्र मौजूद हैं जिनमें अभी डूबना आरंभ भी नहीं किया गया। नहीं कह सकते कि अभी उलूमे-क़ुरआन की कितनी सीपियाँ और उनमें कितने मोती यहाँ हैं। क़ुरआनी तथ्य एवं अन्तर्ज्ञान के समुद्रों में जितनी गहराई तक उतरा गया है, उनका कुछ अंदाज़ा आज की चर्चा से हो जाएगा लेकिन जो नहीं हुई वह उससे बहुत ज़्यादा है जो अब तक हुई है।
आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम सुना होगा जिन का तालुक़ हैदराबाद दक्कन से था और जो फ़्रांस में रहते थे। उन्होंने ख़ुद प्रत्यक्ष रूप से मुझसे यह घटना बताई थी कि संभवतः 1957-58 में एक व्यक्ति उनके पास आया। उनकी ज़िंदगी की यह दिनचर्या थी कि हर-रोज़ दो-चार लोग उनके पास आते और इस्लाम क़ुबूल करते थे। वह भी ऐसा ही एक दिन था कि एक साहब आए और कहा कि मैं इस्लाम क़ुबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने आदत के अनुसार उनको कलिमा पढ़वाया और इस्लाम का संक्षिप्त परिचय उनके सामने पेश कर दिया। अपनी कुछ किताबें उन्हें दे दीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका रोज़ का नियम था कि जब भी कोई उनके हाथ पर इस्लाम क़ुबूल करता था तो वह उससे यह ज़रूर पूछा करते थे कि उसे इस्लाम की किस चीज़ ने प्रभावित किया है।
1948 से 1996 तक यह नियम रहा कि डॉक्टर साहब के मुबारक हाथ पर औसतन दो लोग प्रतिदिन इस्लाम क़ुबूल किया करते थे। आम तौर पर ये लोग इस्लाम के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किया करते थे, वे मिलते-जुलते होते थे। उनमें तुलनात्मक रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास लिख लिया करते थे। इस व्यक्ति ने जो बात बताई वह डॉक्टर साहब के कथनानुसार बड़ी अद्भुत और अलग तरह की थी और मेरे लिए भी बेहद आश्चर्यजनक थी। उसने जो कुछ कहा उसके बारे में डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं इसे बिलकुल नहीं समझा और मैं इसके बारे में कोई फ़न्नी (कलात्मक) राय नहीं दे सकता। उसने बताया “मेरा नाम ज़ाक ज़ेलबीर है। मैं फ़्रांसीसी बोलनेवाली दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने और रिकार्ड फ़्रांसीसी भाषा बोलनेवाली दुनिया में बहुत लोकप्रिय हैं।
आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक अरब राजनयिक के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौक़ा मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोग जमा हो चुके थे और बहुत ही चुपचाप से एक ख़ास अंदाज़ का संगीत सुन रहे थे। जब मैंने वह संगीत सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह तो संगीत की दुनिया की कोई बहुत ही ऊँची चीज़ है जो लोग सुन रहे हैं। मैंने ख़ुद आवाज़ों की जो धुनें और उनका जो उतार-चढ़ाव ईजाद किया है यह संगीत इससे भी बहुत आगे है, बल्कि संगीत की इस सतह तक पहुँचने के लिए अभी दुनिया को बहुत समय दरकार है। मैं चकित था कि आख़िर यह किस व्यक्ति का अविष्कृत किया हुआ संगीत हो सकता है और इसकी धुनें आख़िर किसने कम्पोज़ की हैं। जब मैंने यह मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो लोगों ने मुझे इशारे से ख़ामोश कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझसे रहा न गया और मैंने फिर यही बात पूछी। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे फिर चुप कर दिया”। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस चर्चा के दौरान में वह संगीत कला की कुछ शब्दावली भी प्रयुक्त कर रहा था जिनसे मैं अवगत नहीं, क्योंकि संगीत कला मेरा मैदान नहीं।
कहने का तात्पर्य यह कि जब वह संगीत समाप्त हो गया और वह आवाज़ बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा कि यह सब क्या था? लोगों ने बताया कि यह संगीत नहीं था, बल्कि पवित्र क़ुरआन की तिलावत (पाठ) है और अमुक क़ारी (पाठ करनेवाले) की तिलावत है। संगीतकार ने कहा कि निश्चय ही यह किसी क़ारी की तिलावत होगी और यह क़ुरआन होगा, मगर उसका यह संगीत किस ने कम्पोज़ किया है और यह धुनें किसकी बनाई हुई हैं? वहाँ मौजूद मुसलमान लोग एक साथ बोल पड़े कि “न ये धुनें किसी की बनाई हुई हैं और न ही यह क़ारी साहब संगीत की ए.बी.सी.डी. जानते हैं।” उस संगीतकार ने जवाब में कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि यह धुनें किसी की बनाई हुई न हों। लेकिन उसे यक़ीन दिलाया गया कि पवित्र क़ुरआन का किसी धुन से या संगीत कला से भी कोई संबंध ही नहीं रहा, यह ‘तजवीद’ (क़ुरआन का उच्चारण-ज्ञान) की कला है और एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसने फिर यह पूछा कि अच्छा फिर मुझे यह बताओ कि ‘तजवीद’ और ‘क़िरअत’ की कला कब ईजाद हुई? इस पर लोगों ने बताया कि यह कला तो चौदह सौ साल से चली आ रही है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जब लोगों को पवित्र क़ुरआन प्रदान किया था तो ‘तजवीद’ की कला के सिद्धांतों के साथ ही प्रदान किया था। इसपर उस संगीतकार ने कहा कि अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) ने अपने लोगों को पवित्र क़ुरआन इसी तरह सिखाया है जैसा कि मैंने अभी सुना है तो फिर निस्सन्देह यह अल्लाह की किताब है। इसलिए कि संगीत कला के जो नियम एवं सिद्धांत, क़िरअत की इस शैली में नज़र आते हैं वह इतने उच्च एवं उत्कृष्ट हैं कि दुनिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कहते थे कि मैं उसकी यह बात समझने में असमर्थ था कि वह क्या कह रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाद में मैंने और भी क़ारियों की तिलावते-क़ुरआन को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और विभिन्न लोगों से पढ़वाकर सुना और मुझे यक़ीन हो गया कि यह अल्लाह की किताब है और अगर यह अल्लाह की किताब है तो उसके लानेवाले यक़ीनन अल्लाह के रसूल थे। इसलिए आप मुझे मुसलमान कर लें।
डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसे मुसलमान कर लिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि जो कुछ वह कह रहा था वह किस हद तक दुरुस्त था। इसलिए कि मैं इस कला का आदमी नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने एक अलजज़ाइरी मुसलमान को जो पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस संगीतकार मुसलमान की दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा) के लिए नियुक्त कर दिया। लगभग डेढ़ महीने बाद वे दोनों मेरे पास आए और कुछ परेशान से मालूम होते थे। अलजज़ाइरी शिक्षक ने मुझे बताया कि यह नौ-मुस्लिम पवित्र क़ुरआन के बारे में कुछ ऐसे सन्देह प्रकट कर रहा है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि जिस आधार पर यह व्यक्ति ईमान लाया था वह भी मेरी समझ में नहीं आया था। अब इसके सन्देहों का मैं क्या जवाब दूँगा, और कैसे दूँगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर पूछा कि बताओ तुम्हें क्या शक है? उस नव-मुस्लिम ने कहा कि आपने मुझे यह बताया था और किताबों में भी मैंने पढ़ा है कि पवित्र क़ुरआन ठीक उसी रूप में आज मौजूद है जिस रूप में इसके लानेवाले पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) ने उसे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के सिपुर्द किया था। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि सचमुच ऐसा ही है। अब उसने कहा कि इन साहब ने मुझे अब तक जितना पवित्र क़ुरआन पढ़ाया है उसमें एक जगह के बारे में मुझे लगता है कि इसमें कोई न कोई चीज़ ज़रूर लुप्त हो गई है।
उसने बताया कि उन्होंने मुझे सूरा नस्र पढ़ाई है और इसमें ‘अफ़्वाजा’ और ‘फ़सब्बिह’ के दरमियान ख़ला (रिक्तता) है। जिस तरह कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है वहाँ ‘अफ़्वाजा’ पर ‘वक़्फ़’ किया गया है। ‘वक़्फ़’ करने से वहाँ सिलसिला टूट जाता है जो नहीं टूटना चाहिए। जबकि मेरी कला कहती है कि यहाँ रिक्तता नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहते थे कि यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस सन्देह का जवाब क्या दें और किस तरह सन्तुष्ट करें। कहते हैं कि मैंने तुरन्त मुस्लिम जगत् पर निगाह दौड़ाई तो कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नज़र नहीं आया जो संगीत कला की भी जानकारी रखता हो और ‘तजवीद’ भी जानता हो।
डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ सेकेंड के असमंजस के बाद बिलकुल अचानक और यक-बयक मेरे ज़ेहन में एक पुरानी बात अल्लाह तआला ने डाली कि मैं अपने बचपन में जब मकतब में पवित्र क़ुरआन पढ़ा करता था तो मेरे मुअल्लिम (शिक्षक) ने मुझे बताया था कि ‘अफ़्वाजा’ पर वक़्फ़ नहीं करना चाहिए बल्कि ‘अफ़्वाजा’ को बाद के शब्द से मिलाकर पढ़ा जाए। एक बार मैंने ‘अफ़्वाजा’ पर वक़्फ़ किया था तो इसपर उन्होंने मुझे सज़ा दी थी और सख़्ती से ताकीद की थी कि अफ़्वाजा को आगे मिलाकर पढ़ा करें। मैंने सोचा कि शायद इस बात से इसका सन्देह दूर हो जाए और इसको सन्तोष हो जाए। मैंने उसे बताया कि आपके जो पढ़ानेवाले हैं वह ‘तजवीद’ के इतने माहिर नहीं हैं। दरअस्ल यहाँ इस शब्द को ‘ग़ुन्ना’ (‘अं’ का स्वर) के साथ आगे से मिलाकर पढ़ा जाएगा.... ‘अफ़वाजन फ़सब्बिह’। डॉक्टर साहब का इतना कहना था कि वह ख़ुशी से उछल कर खड़ा हो गया और मुझे गोद में लेकर कमरे में नाचने लगा और कहने लगा कि वाक़ई ऐसे ही होना चाहिए। यह सुनकर उसको मैंने एक दूसरे क़ारी के सिपुर्द कर दिया जिसने उस व्यक्ति को पूरे पवित्र क़ुरआन की शिक्षा दी। वह समय-समय पर मुझसे मिलता था और बहुत सिर धुनता था कि सचमुच यह अल्लाह तआला की किताब है। वह बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ, और एक सफल इस्लामी ज़िंदगी गुज़ारने के बादे 1970 के लगभग उसका इंतिक़ाल हो गया।
इस घटना से मुझे ख़याल होता है कि पवित्र क़ुरआन की जो ‘सौतियात’ (स्वर संबंधी विशेषता) है, यह ज्ञान एवं कला की एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई शोधकर्ता आज तक नहीं उतरा है। और न ही पवित्र क़ुरआन के इस पहलू पर अब तक किसी ने इस अंदाज़ से चिन्तन-मनन किया है। इस घटना के सुनने तक कम से कम मेरा एहसास क्या, ख़याल भी यही था कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र क़ुरआन को बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, ग़ुन्ना, इख़्फ़ा, इज़हार आदि का ख़याल करता है तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन इस कला के इतने अधिक महत्त्व से में इससे पहले अवगत नहीं था। अब मालूम होता है कि ‘तजवीद’ की यह कला भी बेहद महत्त्वपूर्ण चीज़ है।
आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने जो बाद में इस्लाम-दुश्मन साबित हुआ, पवित्र क़ुरआन के शब्द और वाक्यों की संख्या पर कंप्यूटर की सहायता से शोध आरंभ किया था। चूँकि उसने बाद में बहुत-सी ग़लत बातें कहीं और एक गुमराह फ़िर्क़े से उसका संबंध साबित हुआ इसलिए उसकी बात को जल्दी लोग भूल गए और ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कोई 25-30 वर्ष पूर्व पवित्र क़ुरआन के आंकड़ों को कंप्यूटर के आधार पर एकत्र किया था और कोशिश की थी कि वह यह देखे कि पवित्र क़ुरआन में कौन-कौन से शब्द और वाक्य कितनी बार आए हैं और उनमें क्या तत्त्वदर्शिता है। फिर यह कि पवित्र क़ुरआन में जो शब्द आए हैं वे क्यों आए हैं। और जो नहीं आए वे क्यों नहीं आए। इस शोध से उसने बहुत से बिंदु (Points) निकाले।
उदाहरण के लिए उसने एक बात यह खोज की कि पवित्र क़ुरआन की जिन सूरतों के आरंभ में हुरूफ़े-मुक़त्तआत आए हैं उन अक्षरों का हर अक्षर उस सूरा में या तो 19 बार प्रयुक्त हुआ है या इतनी बार कि उसको 19 से बराबर विभाजित किया जा सकता है। लेकिन उस वक़्त उसके महत्त्व का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। उदाहरणार्थ अगर किसी सूरा में ‘ब’ 100 बार इस्तेमाल हुआ हो, और ‘श’ 90 बार तो इससे क्या अन्तर पड़ता है। अलबत्ता उसने कई चीज़ें ऐसी खोजीं जिनसे अंदाज़ा हुआ कि यह बात इतनी महत्त्वहीन भी नहीं है, बल्कि यह इस योग्य है कि इसपर गहराई से चिन्तन करना चाहिए। उदाहरणार्थ उसने कहा कि पवित्र क़ुरआन में हर जगह क़ौमे-लूत का ज़िक्र आया है कि क़ौमे-लूत ने यह किया, और क़ौमे-लूत ने वह क्या। सूरा ‘क़ाफ़’ के आरंभ में ‘क़ाफ़’ जो बतौर हुरूफ़े-मुक़त्तआत के इस्तेमाल हुआ है वह 19 के अदद के साथ संबद्ध है और इस सूरा में पवित्र क़ुरआन का वह एकमात्र स्थान है जहाँ क़ौमे-लूत के बजाय ‘इख़वाने-लूत’ का उल्लेख है। इसलिए कि अगर क़ौमे-लूत का शब्द होता तो ‘क़ाफ़’ का एक अदद बढ़ जाता था। पवित्र क़ुरआन में उसके इस अदद के बार-बार आने का कोई महत्त्व है या नहीं, इससे अलग हटकर इन दो उदाहरणों से यह ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि अभी पवित्र क़ुरआन पर चिन्तन-मनन के नए-नए दरवाज़े खुलने हैं और नई-नई प्रवृत्तियाँ पैदा होनी हैं।
आज की चर्चा में इन दो दिलचस्प भूमिका रूपी उदाहरणों के बाद तफ़सीरे-क़ुरआन में पहले दिन से लेकर अब तक जो बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ सामने आई हैं उनका उल्लेख करना अभीष्ट है। इन प्रवृत्तियाँ में सबसे बड़ी और सबसे नुमायाँ प्रवृत्ति ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ की है। यानी इस बात का प्रबंध करना कि पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर केवल उन रिवायतों के आधार पर की जाए जो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से उल्लिखित हैं। उनके अलावा किसी और उद्धरण-स्रोत, या किसी और तफ़सीरे-क़ुरआन के मूल स्रोत के मामले में प्रभावी होने की अनुमति न दी जाए। यहाँ तक कि अरबी भाषा, उसके मूलस्रोत, निजी राय, सोच और अन्तर्दृष्टि किसी चीज़ को इसमें दख़ल देने की अनुमति न दी जाए। यह प्रवृत्ति आरंभ में यानी शुरुआती दो-तीन सदियों में तफ़सीरे-क़ुरआन की सबसे मज़बूत और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति के ज़्यादा मज़बूत और लोकप्रिय होने की एक वजह तो यह है कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से आनेवाली महत्त्वपूर्ण तफ़सीरी पूँजी लोगों के सामने मौजूद थी और ताबिईन ने उसको बहुत विस्तार, सावधानी और मेहनत से संकलित कर दिया था। दूसरी वजह यह है कि उस ज़माने के विद्वानों का अत्यंत अल्लाह से डरनेवाला और अत्यंत सावधानीपूर्ण रवैया भी इस प्रवृत्ति के फलने में सहयोगी सिद्ध हुआ कि वह ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ के अलावा किसी और अंदाज़ की तफ़सीर के काम को प्रोत्साहित करें। इसलिए जितनी भी तफ़सीरें आरंभिक सदियों में लिखी गईं वे अधिकतर ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ ही की शैली की लिखी गईं। यानी तमाम तफ़सीरी उल्लेखों को एकत्र करके और उनको सामने रखकर क़ुरआनी आयत की तफ़सीर बयान कर दी जाए।
‘तफ़सीर बिल-मासूर’ के नाम से जो सामग्री जमा हुई वह निस्सन्देह तफ़सीर के सबसे महत्त्वपूर्ण मूल स्रोतों में से एक है। बहुत-सी तफ़सीरें ऐसी हैं जो सिर्फ ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ के आधार पर लिखी गईं। लेकिन कुछ तफ़ासीरें ऐसी भी हैं, मुताख़्ख़िरीन (बाद में आनेवाले विद्वानों) के यहाँ भी और अधिकतर मुतक़द्दिमीन (प्राचीन विद्वानों) के यहाँ भी जिनका अस्ल दारोमदार तो ‘मासूर’ (विश्वसनीय उल्लेखों) पर है। लेकिन उन्होंने शेष स्रोतों पर भी कुछ न कुछ ध्यान दिया है।
लेकिन ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ के सारे महत्त्व के बावजूद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, दूसरी शताब्दी हिजरी के बाद किसी हद तक और तीसरी शताब्दी हिजरी के बाद व्यापक स्तर पर ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ में कमज़ोर रिवायतें शामिल होने लगीं। दुनिया का आम नियम और देखी हुई बात है कि जो चीज़ लोकप्रिय हो और बाज़ार में चल रही हो उसमें धोखेबाज़ भी शामिल होने लगते हैं। यह हर इंसानी प्रयास के साथ होता है कि जिस चीज़ का बाज़ार में चलन हो उसमें जालसाज़ और दो नंबर का माल पैदा करनेवाले भी घुस जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अस्ल चीज़ भी कहीं न कहीं मौजूद है। मौलाना जलालुद्दीन रुमी (रहमतुल्लाह अलैह) की एक बहुत ही सूक्ष्म बात है, मुझे पसंद आई। उन्होंने किसी जगह बयान किया है कि इंसान को किसी प्रशिक्षक को तलाश करके उसके पास अपने प्रशिक्षण के लिए जाना चाहिए। किसी ने कहा कि आजकल तो जालसाज़ बहुत पैदा हो गए हैं और प्रशिक्षण के नाम पर चालिबाज़याँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात का प्रमाण है कि अस्ल लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ार में जाली सिक्का उसी समय चलता है जब उस बाज़ार में अस्ली सिक्का भी मौजूद हो। जिस बाज़ार में अस्ली सिक्का नहीं होगा वहाँ नक़्ली भी नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र का यह बड़ा ज़बरदस्त सिद्धांत है, जो बाद में खोजा गया, लेकिन मौलाना ने उसको सबसे पहले बयान किया।
चूँकि ‘तफ़सीर बिल-मासूर’ सिक्का-ए-राइज-उल-वक़्त (प्रचलित रीति) था और ज्ञान की दुनिया में इसका चलन था। इसलिए बहुत-से अल्पज्ञानी और कुछ जालसाज़ भी मैदान में आ गए और उन्होंने बहुत ही कमज़ोर रिवायतें भी फैला दीं। इन कमज़ोर रिवायतों का मूलस्रोत ‘इसराईलियात’ (यहूदियों और ईसाइयों के धर्मग्रन्थों में वर्णित अप्रमाणित कहानियाँ) थीं। मुतक़द्दिमीन (प्राचीन विद्वान) तो जब तक ताबिईन और तबा-ताबिईन का ज़माना था, इसराईली रिवायतों से क़ुरआन की तफ़सीर (टीका) बयान करने में बहुत ही सावधानी से काम लेते थे। उन्होंने ‘इसराईलियात’ को क़ुबूल करने और आगे बयान करने में हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम लिया था। बाद में न ज़िम्मेदारी की वह सतह बाक़ी रही और न सावधानी की ऐसे स्तर का ध्यान रखा जा सका। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूर्ण निष्ठाभाव से भी बहुत ही कमज़ोर चीज़ें स्वीकार कर लीं। कमज़ोर रिवायतों के बारे में यह न समझिएगा कि जिन लोगों ने यह कमज़ोर रिवायतें बयान कीं वे सारे के सारे जालसाज़ और बेईमान थे। ऐसा नहीं है। निश्चय ही कमज़ोंर रिवायतें बयान करनेवालों में कई जालसाज़ भी थे, उनमें कई बेईमान भी थे, इस्लाम-दुश्मन भी थे। लेकिन उनमें से बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने बड़े ही निष्ठाभाव से कमज़ोर रिवायतों को स्वीकार कर लिया। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हवाले से कोई ऐसी चीज़ बयान करते सुना जिससे किसी नैतिक मूल्य का समर्थन होता हो तो उन्होंने उसे तुरन्त अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) का कथन (हदीस) समझकर क़ुबूल कर लिया और यह सोचा ही नहीं कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) के मुबारक नाम का हवाला देकर कोई झूठ भी बोल सकता है। अब उन्होंने इस कमज़ोर बात को आगे बयान करना आरंभ कर दिया। यों निष्ठाभाव से भी कमज़ोर रिवायतें दाख़िल हो गईं। लेकिन यह वह निष्ठाभाव था जिसमें विवेक शामिल नहीं था। इसी लिए अगर निष्ठाभाव के साथ विवेक और अन्तर्दृष्टि भी शामिल हो, तभी काम चलता है, मात्र निष्ठाभाव काम नहीं आता। इन कारणों के आधार पर बहुत ही कमज़ोर रिवायतें तफ़सीर बिल-मासूर के साहित्य में शामिल हो गईं।
तफ़सीर बिल-मासूर का सबसे बड़ा मूलस्रोत, सबसे पुरानी तफ़सीरों में तारीख़े-तबरी है। इसमें प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से आई हुई तमाम रिवायतों को जमा किया गया और सुरक्षित कर दिया गया। तफ़सीरे-तबरी में ‘इसराईलियात’ भी अच्छी-ख़ासी संख्या में शामिल हैं। लेकिन वे ‘इसराईलियात’ हैं जिनके बारे में इमाम तबरी का विचार था कि वे स्वीकार्य हैं और उन रिवायतों में कोई चीज़ आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि यह इमाम तबरी की निजी राय थी, जिसको बाद में आनेवाले बहुत-से लोगों ने स्वीकार भी किया और बहुत-सों ने इससे मतभेद भी किया। जिस तरह इमाम तबरी को ‘इसराईलियात’ के बारे में एक राय क़ायम करने का हक़ है, उसी तरह बादवालों को भी हक़ था कि अपनी जाँच-पड़ताल के अनुसार राय क़ायम करें। ‘इसराईलियात’ के बारे में उन्हें स्वीकार करने से यह ज़रूर मालूम होता है कि मुसलमानों का स्वभाव ज्ञानपरक विशालता का है। यानी ज्ञान में विशाल और विशाल हृदयता हमेशा मुसलमानों का विशेष गुण रहा है। मुसलमानों ने कभी दूसरों से कोई ज्ञानरकत चीज़ हासिल करने में किसी पक्षपात का प्रदर्शन नहीं किया। अतीत में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी मसीही लेखक ने या किसी यहूदी या हिंदू लेखक ने अपने किसी धर्म ग्रन्थ की व्याख्या या समर्थन में मुसलमानों के किसी दृष्टिकोण को बयान किया हो और अपनी किसी धार्मिक चीज़ के समर्थन में पवित्र क़ुरआन या मुसलमानों के दृष्टिकोण से काम लिया हो। इससे उनके पक्षपात का अंदाज़ा होता है। लेकिन इस अपक्षपाती नीति से कुछ लोगों ने बहुत ग़लत लाभ उठाया और ऐसी चीज़ें मुसलमानों में फैला दीं जो इस्लामी अक़ीदों (धारणाओं) और इस्लामी शिक्षाओं के अनुकूल नहीं थीं। अब यह बात कि किसने ये चीज़ें फैलाईं यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी की नीयत के बारे में फ़ैसला करना उचित नहीं है।
इसराईली रिवायतों को मुसलमान विद्वानों में लोकप्रिय बनाने में कुछ लोगों को ख़ास ख्याति प्राप्त हुई। जो नाम इस पूरी प्रक्रिया में बहुत नुमायाँ रहे हैं उनमें एक नाम पर बहुत बहस हुई है, वह थे काबुल-अहबार। यह साहब यहूदियों के एक बड़े विद्वान थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) के ज़माने में अरब में मौजूद थे, लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) के ज़माने में उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में कहीं जाकर वह मुसलमान हुए। मुसलमानों में जल्द ही उनको बहुत सम्मानित स्थान प्राप्त हो गया। वह अपनी पिछली मज़हबी रिवायतों को बयान किया करते थे और मुसलमानों में बहुत-से लोग दिलचस्पी से बैठकर उनकी रिवायतों को सुना करते थे। इस तरह बहुत-सी बातें उनके हवाले से मशहूर हो गईं और धीरे-धीरे क़ुरआन के टीका संबंधी साहित्य में बहुत-सी चीज़ें शामिल हो गईं। वह किस दर्जे के इंसान थे? इस्लाम के प्रति कितने निष्ठावान थे? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। कुछ लोगों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणियाँ की हैं और कुछ लोगों ने नकारात्मक टिप्पणियाँ की हैं। हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मशहूर टीकाकार, इतिहासकार और हदीसों के ज्ञाता अल्लामा इब्ने-कसीर जो इल्म और तक़वा (ज्ञान एवं ईश-परायणता) दोनों में अत्यंत उच्च स्थान रखते हैं, और इल्मे-तफ़सीर में, इतिहास में और फ़िक़्ह में यानी हर कला में उच्च स्थान रखते हैं और अपने ज़माने के पहली पंक्ति के विद्वानों में से हैं, उन्होंने अपनी तफ़सीर में लिखा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ इस उम्मत (समुदाय) को काबुल-अहबार की तरफ़ से आनेवाले किसी इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इस वाक्य में बहुत कुछ कह दिया गया है। अगरचे इस वाक्य में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उनकी रिवायतों का ज्ञानपरक और धार्मिक महत्त्व स्पष्ट कर दिया गया।
तफ़सीर बिल-मासूर के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि शुरू-शुरू में जब यह प्रवृत्ति सामने आई तो इस प्रवृत्ति का इल्मे-हदीस से बड़ा गहरा संबंध था। क्योंकि हदीस के भंडारों ही में से तफ़सीरी भंडार भी आ रहे थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) से जो कुछ बातें रिवायत हुई थीं वे सारी की सारी इल्मे-हदीस में संकलित हो रही थीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मुबारक वुजूद से जुड़े इन उद्धरणों में तफ़सीरी उद्धरण भी शामिल थे। इसलिए शुरू-शुरू में इल्मे-हदीस और तफ़सीर बिल-मासूर एक ही चीज़ के मानो दो नाम थे। चुनाँचे आज भी आप हदीस की कोई किताब उठाकर देख लें। वह इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) की जामे-सहीह हो, या इमाम तिरमिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) की जामे या कोई और हदीस-संग्रह, आपको उनमें से हर एक किताब में तफ़सीरी सामग्री पर आधारित एक अध्याय ज़रूर मिलेगा। जो सारा का सारा तफ़सीर बिल-मासूर ही पर आधारित होगा। फिर जितनी विश्वसनीय वह किताब होगी उतनी ही विश्वसनीय उसमें शामिल तफ़सीरी सामग्री का दर्जा होगा। चुनाँचे बुख़ारी का तफ़सीरी हिस्सा हदीसों के दूसरे संग्रहों के तफ़सीरी संग्रहों और रिवायतों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो तफ़सीरी पूँजी सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम दोनों में है वह हदीस की शेष किताबों की तफ़सीरी सामग्री से अधिक विश्वसनीय है। जो इन दोनों में किसी एक में है वह भी शेष किताबों से तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय है।
समय बीतने के साथ-साथ तफ़सीर बिल-मासूर का विभाग इल्मे-हदीस से अलग भी एक विभाग के तौर पर जाना जाने लगा और एक ज़माना ऐसा आया कि इल्मे-हदीस इस इल्म के एक मूल स्रोत के तौर पर तो रहा, लेकिन इस इल्म ने, इल्मे-हदीस से अलग एक विभाग का रूप ले लिया। ज्ञान के इस विभाग में हदीस के अलावा भी अन्य माध्यमों से सामग्री आती गई और किताबें लिखी जाती रहीं।
इस तफ़सीरी भंडार की वजह से, ख़ास तौर पर ‘इसराईलियात’ के कारण मुसलमानों में बहुत-से ऐसे सवाल भी पैदा हुए जो नहीं पैदा होने चाहिएँ थे। उदाहरण के रूप में एक चीज़ बताता हूँ। हर मुसलमान यह समझता है कि इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने जिस बेटे की क़ुरबानी दी वह इस्माईल (अलैहिस्सलाम) थे और इसमें किसी को भी कोई शक नहीं। लेकिन जब ‘इसराईलियात’ का आना आरंभ हुआ तो चूँकि इसराईली यह कहते थे कि ‘ज़बीह’ इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) थे, यानी इबराहीम (अलैहिस्सलाम) उन्हें ही ज़ब्ह करने के लिए ले गए थे, इसलिए मुसलमानों में भी ऐसी ग़लतफ़हमी पैदा होनी आरंभ हो गई। यहूदियों ने यह दावा क्यों किया? इसका कारण संभवतः यह है कि यह इतनी बड़ी और महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की ज़िंदगी में इतनी बेमिसाल क़ुरबानी है कि यहूदी यह चाहते थे कि इस अज़ीमुश्शान घटना के हवाले में उनके जिस बेटे का नाम आए वह अरबों के पूर्वज इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के बजाय यहूदियों के पूर्वज इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) हों। इसलिए उन्होंने इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) के नाम से ये रिवायतें फैलानी आरंभ कर दीं। और उन रिवायतों में से सौ प्रतिशत रिवायतों के रावी काबुल-अहबार थे। इस वजह से बहुत-से मुसलमानों को यह ख़याल हो गया कि शायद इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) ही ‘ज़बीह’ होंगे। अतः मुसलमान लेखकों को इस स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ी कि ‘ज़बीह’ कौन-से बेटे हैं। इस सिलसिले में मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही की एक संक्षिप्त पुस्तिका है ‘अर्राय अस्सहीह फ़ी मन हु-व अज़-ज़बीह’। इस किताब में उन्होंने न केवल पवित्र क़ुरआन से, बल्कि बाइबल और तौरात से मज़बूत तर्क देकर यह साबित किया है कि इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ही ‘ज़बीह’ थे। इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के ‘ज़बीह’ होने की एक दलील तो ऐसी है जिसका किसी यहूदी और ईसाई के पास कोई जवाब नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अल्लाह ने इबराहीम से कहा कि अपने इकलौते बेटे की क़ुरबानी दें। यानी जिस बेटे की क़ुरबानी दी वह इकलौते थे। इसके बाद एक और जगह बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक़ पैदा हुआ तो इस्माईल दस वर्ष का था और उसके साथ ठट्ठा करता था। इसका मतलब यह हुआ कि इसमाईल (अलैहिस्सलाम) पहले पैदा हुए और इसहाक़ (अलैहिस्सलाम) से दस साल बड़े थे। और इकलौते भी वही थे जो पहले पैदा हुए। और क़ुरबानी इकलौते बेटे की दी गई। इसलिए बाइबल ही से मालूम होता है कि ‘ज़बीह’ इसहाक़ नहीं थे, बल्कि इस्माईल थे।
जो तफ़सीरें ‘मासूर’ प्रवृत्तियों पर लिखी गईं उनमें से दो का कुछ विस्तृत उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। यानी अल्लामा तबरी की तफ़सीरे-तबरी और अल्लामा इब्ने-कसीर की तफ़सीर इब्ने-कसीर। तफ़सीर बिल-मासूर के विषय पर एक और तफ़सीर है जो तुलनात्मक रूप से बाद में लिखी गई, लेकिन वह इस दृष्टि से बहुत अलग है कि उसमें पूरे मासूरी (उल्लेखों पर आधारित) साहित्य का अध्ययन करके पूरी उपलब्ध सामग्री को समोने की कोशिश की गई है। यह किताब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की ‘अद्दुर्रुल-मंसूर’ है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती (रहमतुल्लाह अलैह) मशहूर मुफ़स्सिर, मुहद्दिस और फ़क़ीह, बल्कि ऑल राउंडर व्यक्ति थे, जिनकी कमो-बेश पाँच सौ किताबें मौजूद हैं। उन्होंने ‘अद्दुर्रुल-मंसूर फ़ित-तफ़सीर बिल-मासूर’ भी लिखी, यह तफ़सीर हर जगह मिलती है। इसके विभिन्न एडिशन निकल चुके हैं। इस किताब में उन्होंने पूरे तफ़सीरी भंडार से मासूरी साहित्य को इकट्ठा करके एक किताब में जमा कर दिया है। ‘अल-इतक़ान फ़ी उलूमिल-क़ुरआन’ जो उलूमे-क़ुरआन पर अल्लामा सुयूती की प्रसिद्ध किताब है, उसी का प्राक्कथन है, जो एक-एक और दो-दो भागों में अलग से कई बार छपी है। संभवतः अद्दुरुल-मंसूर का उर्दू अनुवाद भी कोई दो ढाई सौ साल पूर्व हो चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज़ों के आगमन से पहले किसी बुज़ुर्ग ने किया था। यह मुग़ल साम्राज्य के आख़िरी दौर की बात है।
एक और किताब का उल्लेख यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो इस दृष्टि से बहुत अनोखी है कि अहले-सुन्नत के तमाम वर्गों और शीया लोगों, दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। यह एक ऐसे लेखक की है कि मसलक की दृष्टि से उनका संबंध अहले-सुन्नत से नहीं, बल्कि ज़ैदी शीया फ़िर्क़े से था। लेकिन उनकी किताबों को अधिक लोकप्रियता अहले-सुन्नत ही में प्राप्त हुई। यह लेखक यमन के अल्लामा मुहम्मद-बिन-अली शौकानी हैं। इनका संबंध तेरहवीं हिजरी शताब्दी के आरंभ से है। अधिक पुराने नहीं हैं। इनका संबंध फ़िक़्ह-ज़ैदी से था, जो शीया फ़िक़्ह (धर्मशास्त्र) की एक कुछ सन्तुलित शाखा है। इस फ़िक़्ह के बड़े गहरे प्रभाव यमन में आज भी मौजूद हैं। अल्लामा शौकानी की किताबें विशेष रूप से उनकी तफ़सीर ‘फ़तहुल-क़दीर’ बड़ा ज्ञानपरक स्थान रखती है। उसको मुस्लिम जगत् में हर जगह लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी एक और किताब ‘नीलुल-औतार’ भी प्रसिद्ध है। यह आदेशोंवाली हदीसों का बहुत उत्कृष्ट संग्रह और व्याख्या है, यानी फ़िक़्हुल-हदीस की किताब है। नीलुल-औतार का उर्दू अनुवाद हो गया है, और हमारी यूनिवर्सिटी (अंतरराष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय इस्लामाबाद) की शरीआ अकैडमी उसको प्रकाशित कर रही है। अल्लामा शौकानी की एक किताब उसूले-फ़िक़्ह पर भी है जो दुनिया की हर इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वह शीया हो या सुन्नी हो, पढ़ाई जाती है। अल्लामा शौकानी मुस्लिम जगत् के एक ऐसे निराले व्यक्तित्व हैं जो मुस्लिम जगत् के हर मसलक के लिए सम्मान योग्य हैं, और व्यावहारिक रूप से उनकी किताबों से हर जगह लाभ उठाया जाता है। उनकी किताब ‘फ़तहुल-क़दीर’ भी तफ़सीरे-मासूर के अंदाज़ में लिखी जानेवाली आख़िरी उल्लेखनीय किताब है। इस किताब की तैयारी में उन्होंने बहुत-सी किताबों से लाभ उठाया है, जिनमें अल्लामा सुयूती की ‘अद्दुर्रुल-मंसूर’ भी शामिल है।
तफ़सीर की दूसरी प्रवृत्ति जो ऐतिहासिक दृष्टि से तफ़सीर बिल-मासूर के बाद दूसरी प्रवृत्ति है, वह तफ़सीर का शब्दकोशीय और साहित्यिक अंदाज़ है। पवित्र क़ुरआन स्पष्ट अरबी में है और मक्का के क़ुरैश की उच्चस्तरीय और टकसाली ज़बान में है। बहुत-से लोगों ने अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ इस काम के लिए समर्पित कीं कि पवित्र क़ुरआन को समझने के लिए जिन शैलियोँ की जानकारी दरकार है उन सबके बारे में अरब क़बीलों में फिरकर जानकारियाँ एकत्र की जाएँ और उस साहित्य को जमा किया जाए। जैसे-जैसे यह साहित्य इकट्ठा होता गया इस विषय पर किताबें तैयार होती गईं। आख़िरकार एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार हो गई जिसमें पवित्र क़ुरआन की शाब्दिक और साहित्यिक तफ़सीरें हैं। इन किताबों में प्राचीनतम किताब ‘मजाज़ुल-क़ुरआन’ के नाम से अबू-उबैदा मुअम्मर-बिन-अल-मुसन्ना की है। उनके ज्ञानपरक स्थान और साहित्यिक रुतबे के बारे में इतना बता देना काफ़ी है कि इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब में बीसियों जगह उनका हवाला दिया है और उनकी जमा की हुई तफ़सीरी सामग्री से लाभ उठाया है।
हाफ़िज़ इब्ने-हजर अस्क़लानी का उलूमे-हदीस के इतिहास में जो दर्जा है वह किसी से छिपा नहीं है। हदीस के व्याख्याताओं में उनसे ऊँचा दर्जा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इब्ने-ख़लदून ने एक जगह लिखा है (इब्ने-ख़लदून का ज़माना हाफ़िज़ इब्ने-हजर से थोड़ा ही पहले है) कि बुख़ारी जिस शान की किताब है, उसी शान की उसकी शरह (व्याख्या) अभी तैयार नहीं हुई और यह पूरी उम्मते-मुस्लिमा (मुस्लिम समुदाय) के ज़िम्मे एक क़र्ज़ है। जब ‘फ़तहुल-बारी’ लिखी गई तो मुस्लिम जगत् ने सर्वसम्मति से यह कहा कि इब्ने-ख़लदून ने जिस क़र्ज़ का उल्लेख किया था, वह फ़तहुल-बारी के रूप में उतारा जा चुका है। इसके बाद सहीह बुख़ारी की इससे अच्छी व्याख्या नहीं पाएँगे। एक प्रसिद्ध हदीस है ‘ला हिजर-त बादल-फ़तह’। यानी जब मक्का फ़तह हो गया तो हिजरत अब अनिवार्य नहीं रही।
इन हाफ़िज़ इब्ने-हजर ने अबू-उबैदा की पूरी किताब ‘मजाज़ुल-क़ुरआन’ को अपनी किताब में समो दिया है और मजाज़ुल-क़ुरआन में अब शायद ही कोई ऐसी सामग्री बाक़ी रह गई होगी जो हाफ़िज़ इब्ने-हजर की किताब में बिखरी हुई न हो। अबू-उबैदा का इंतिक़ाल 210 हिजरी में हुआ। इनकी उम्र लगभग इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) के बराबर थी। इन्हीं के एक और समसामयिक थे यह्या-बिन-ज़ियाद अल-फ़रा। उनकी किताब ‘मआनिउल-क़ुरआन’ पाँच भागों में है। यह अपनी जगह बहुत बड़े साहित्यकार और सर्फ़-ओ-नह्व (अरबी व्याकरण) के इमाम थे।
यह्या-बिन-ज़ियाद अल-फ़रा की ‘मआनिउल-क़ुरआन’ इस कला की सर्वप्रथम और अत्यंत महत्त्वपूर्ण किताबों में है। पवित्र क़ुरआन के शाब्दिक सौंदर्य और साहित्यिक शैलियोँ पर सबसे पहले जिस मुफ़स्सिर (टीकाकार) ने सारगर्भित कार्य किया वह यही फ़रा थे जिनको उनके ज़माने में ‘अमीरुल-मोमिनीन फ़िन-नह्व’ यानी अरबी व्याकरण के विशेषज्ञ कहा जाता था। उनकी इस किताब मआनिउल-क़ुरआन की गणना पहले रोज़ से ही इस विषय की सर्वोत्तम रचनाओं में की गई। वह इस किताब का आम दर्स भी दिया करते थे जिसमें बड़ी संख्या में विद्वान भी शरीक हुआ करते थे।
ये दोनों किताबें यानी अबू-उबैदा की ‘मजाज़ुल-क़ुरआन’ और फ़रा की ‘मआनिउल-क़ुरआन’ शाब्दिक दृष्टि से पवित्र क़ुरआन की व्याख्या और तफ़सीर का सर्वप्रथम उद्धरण स्रोत समझी जाती हैं। उनके बाद और भी किताबें पवित्र क़ुरआन की शब्दकोशीय बहसों पर लिखी गईं। लेकिन जो सामग्री उन्होंने यानी अबू-उबैदा और यह्या-बिन-ज़ियाद अल-फ़रा ने संकलित कर दी थी वह बाद के तमाम टीकाकारों के सामने रही। यहाँ तक कि उर्दू भाषा के मुफ़स्सिरीने-क़ुरआन ने भी अल-फ़रा की मआनिउल-क़ुरआन से लाभ उठाया है। जैसे कि मौलाना मौदूदी, मौलाना इस्लाही, मौला मुहम्मद इदरीस कांधलवी, मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी आदि की तफ़सीरों में इससे लाभ उठाने की झलक महसूस होती है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनका काम कितना बहुमूल्य था।
इसके बाद जब ये दोनों तरह की सामग्रियाँ जमा हो गईं, यानी तफ़सीर बिल-मासूरी और तफ़सीर बिल-अदब (अरब साहित्य के आधार पर क़ुरआन की टीका) भी, तो एक तीसरी प्रवृत्ति सामने आई, जिसके बारे में बड़ी लम्बी बहसें हुईं कि इस प्रवृत्ति को जन्म लेने और पनपने की इजाज़त दी जाए या न दी जाए। यह प्रवृत्ति ‘तफ़सीर-बिर्राय’ की थी। यानी मुफ़स्सिर अपनी राय, अन्तर्दृष्टि और इजतिहाद के अनुसार भी पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर करे और उपलब्ध सामग्री से भी काम ले। अभी तक यह रिवाज था कि पवित्र क़ुरआन की आयत की तफ़सीर बड़े सादा से अंदाज़ से की जाती थी। जैसे ‘अनअम-त अलैहिम’ का ज़िक्र आया तो वह आयत नक़्ल कर दी जिसमें ईनाम पानेवाले ख़ुश-नसीबों का स्पष्टीकरण है। ‘ग़ैरिल-मग़ज़ूबि’ और ‘ज़ाल्लीन’ का ज़िक्र आया तो वह हदीस पेश कर दी जिसमें बताया गया है कि ‘मग़ज़ूब अलैहिम’ से मुराद यहूदी और ‘ज़ाल्लीन’ से मुराद ईसाई हैं, या अगर कोई शब्दकोशीय या साहित्यिक चीज़ हासिल थी, वह बयान कर दी। इससे अधिक मुफ़स्सिरीन आगे नहीं बढ़े थे। उनकी असाधारण सावधानी, उनका असाधारण तक़वा (परहेज़गारी), उनकी विनम्रता और ज़िम्मेदारी का गहरा एहसास उनको इसकी इजाज़त नहीं देता था कि वह अपने किसी निजी विचार को इस योग्य भी समझें कि इससे पवित्र क़ुरआन के समझने में काम लिया जा सकता है।
जब यह सारी सामग्री संकलित हो गई और तफ़सीर बिल-मासूर और तफ़सीर-बिल्लुग़त पर किताबें उपलब्ध हो गईं तो अब लोगों ने एक क़दम और आगे बढ़ाया और तफ़सीर-बिर्राय से भी काम लेना आरंभ किया। तफ़सीर-बिर्राय के बारे में तीन दृष्टिकोण पैदा होने आरंभ हुए। एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण तो यह था कि तफ़सीर-बिर्राय एक बिलकुल ग़लत प्रवृत्ति है, इससे बड़ी ख़राबियाँ पैदा होंगी, इसलिए उसकी सिरे से इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि तफ़सीर का यह अंदाज़ मुसलमानों में ग़लतफ़हमी का रास्ता खोलेगा। पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर जैसा गंभीर काम बच्चों का खेल बन जाएगा और हर ऐरा-ग़ैरा उठकर अपनी राय के अनुसार अल्लाह की किताब के अर्थ बताने की कोशिश करेगा। मुतक़द्दिमीन (प्राचीन विद्वानों) में से अधिकतर लोगों की यही राय थी और उन्होंने इसके लिए मज़बूत तर्क भी दिए।
जब मुताख़्ख़िरीन (बाद के विद्वानों) का दौर आया तो उनमें दो दृष्टिकोण सामने आए। एक सन्तुलित प्रवृत्ति यह थी कि तफ़सीरे-बिर्राय का पूरी तरह विरोध न किया जाए, बल्कि यह देखा जाए कि जो राय दी जा रही है वह अपनी जगह क्या हैसियत रखती है। अगर वह राय स्वीकार करने योग्य है जिसको वह ’राय महमूद’ (प्रशंसनीय राय) कहा करते थे तो ठीक है। और अगर राय ग़लत है जिसको वह ‘राय मज़मूम’ (निंदनीय राय) का नाम देते थे तो वह स्वीकार्य नहीं है। तीसरी प्रवृत्ति जो बहुत थोड़े-से लोगों की थी यह थी कि इंसान की हर राय सम्मान योग्य है। पवित्र क़ुरआन ने ख़ुद उसके महत्त्व को स्वीकार किया है, चिन्तन-मनन का उपदेश जगह-जगह दिया गया है। राय और नज़र की दावत दी है, बुद्धि, चिन्तन और गहन विचार पर बल दिया गया है। इसलिए किसी भी राय का रास्ता नहीं रोकना है।
अन्ततः मुस्लिम समुदाय में न तो आख़िरी राय को प्रोत्साहन मिला, और न पहली राय को अधिक समय तक स्वीकार किया गया। मुस्लिम समुदाय ने इन दोनों रायों को क़ुबूल नहीं किया, बल्कि एक बीच का रास्ता अपनाते हुए अच्छी राय और बुरी राय में भेद किया। पसंदीदा राय के आधार पर तफ़सीरें लिखी गईं और संकलित हुईं। लेकिन ज़रा ग़ौर किया जाए तो पता चलता है कि पहलेवाले विद्वानों में से जिन लोगों ने तफ़सीर-बिर्राय का विरोध किया या उसको रद्द किया, वे पूरे तौर पर राय और इज्तिहाद के विरोधी नहीं थे, बल्कि तफ़सीर-बिर्राय के बारे में उनमें से लगभग सबकी राय वही थी जो बादवाले विद्वानों की राय थी। वे यह समझते थे कि यहाँ तफ़सीर-बिर्राय से मुराद वह राय है जो अन्दाज़े और अटकल पर आधारित हो। और लोगों की निजी पसंद और नापसंद पर इसका दारोमदार हो, इसी राय के बारे में वे लोगों से कहते थे कि लोग अपनी निजी इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार राय देने लगेंगे। ऐसी राय निश्चय ही अस्वीकार्य है।
बादवाले विद्वानों और पहले के विद्वानों, दोनों के निकट केवल वह राय स्वीकार्य है जो सही ज्ञानपरक प्रयास और धार्मिक अन्तर्दृष्टि पर आधारित हो, वह राय जो शान्तिप्रिय दिल और सद्बुद्धि के अनुसार हो, और क़ुरआन और सुन्नत की सीमाओं के अंदर-अंदर हो, ऐसी राय निस्सन्देह सब के निकट स्वीकार्य है। इसके मुक़ाबले में जो राय नापसंदीदा और निंदनीय है वह राय है जिसका आधार मात्र अटकलों पर हो। इसलिए कि पवित्र क़ुरआन ने अटकलों को इल्म का ज़रिया नहीं माना, إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا अर्थात् “निश्चय ही अटकल कदापि सत्य का बदल नहीं हो सकती।” (क़ुरआन, 10:36) एक जगह है, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ अर्थात् “और जिस चीज़ का तुम्हें ज्ञान न हो उसके पीछे न लगो।” (क़ुरआन, 17:36) अतः अटकलों के आधार पर जितनी रायें हैं वे चूँकि ज्ञान एवं विश्वास पर आधारित नहीं हैं, इसलिए उन्हें पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर में डाल देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
ये लोग अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के एक प्रसिद्ध कथन का भी हवाला देते थे। किसी व्यक्ति ने उनसे पवित्र क़ुरआन की किसी आयत का अर्थ पूछा तो आपने जवाब दिया कि मुझे इस मामले में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कोई कथन मालूम नहीं। पूछनेवाले ने कहा कि फिर आप अपने विवेक और समझ के अनुसार उसका जवाब दे दीजिए तो उन्होंने जवाब दिया, “कौन-सा आसमान मुझपर छाया करेगा और कौन-सी ज़मीन मुझे ठिकाना देगी अगर मैं पवित्र क़ुरआन के बारे में अपनी राय से काम लूँ।” गोया उन्होंने न केवल अपनी राय से काम लेने से इनकार कर दिया, बल्कि निजी राय से पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर करने को एक बड़ा दुस्साहस भी ठहरा दिया। यही वजह है कि नेक बुज़ुर्गों में से अधिकतर लोग इस मामले में असाधारण सावधानी और सख़्ती से काम लिया करते थे।
मशहूर ताबिई सईद-बिन-मुसय्यिब पहली सदी के अन्त के नामवर विद्वानों में से थे। वे ताबिईन में बहुत ऊँचा दर्जा रखते हैं। बल्कि ताबिईन में जो कुछ व्यक्ति नेतृत्व के स्थान पर आसीन थे, उनमें से एक थे, वह एक लम्बे समय तक अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के साथ रहे, उनके शिष्य थे और बाद में उनके दामाद भी बने। एक लम्बे समय तक दर्स देने और शिक्षण कार्य में मदीना मुनव्वरा में व्यस्त रहे, लोग आते और उनसे फ़िक़्ह और हदीस के बारे में सवाल करते और वह जवाब देते। लेकिन जब कोई व्यक्ति उनसे पवित्र क़ुरआन की किसी आयत की तफ़सीर के बारे में कुछ पूछता तो ऐसे हो जाते जैसे उन्होंने सुना ही नहीं।
ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग सावधानी, तक़्वा (ईशपरायणता) और विनम्रता की पराकाष्ठा के कारण कोई राय व्यक्ति करने से बचते थे, हालाँकि ज्ञान के जिस उच्च स्थान पर आसीन थे उसका अंदाज़ा सबको है।
अब्दुल-मलिक अस्मई, जिनका मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, वह लम्बे समय अरब के रेगिस्तानों में फिरते रहे कि पवित्र क़ुरआन के अर्थों से संबंधित शब्दकोश तथा साहित्य के उदाहरण एकत्र करें। जब उनसे कोई व्यक्ति पवित्र क़ुरआन की किसी आयत के अर्थ पूछता था तो कहा करते थे कि पवित्र क़ुरआन के शब्द के अर्थ तो मालूम नहीं, लेकिन अरब इस शब्द को इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कोई ग़लती हो जाए, एक प्रति हज़ार भी तो वह पवित्र क़ुरआन से जुड़ न पाए। हालाँकि जो वह कहते थे वह सौ प्रतिशत होता था। इसी असाधारण सावधानी प्रियता के कारण तफ़सीर-बिर्राय को प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन और तबा-ताबिईन के दौर में ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त न होगी। लेकिन ख़ुद उन लोगों के ज़माने में भी कई अवसर ऐसे आए कि उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में अपनी राय दी, मुस्लिम समुदाय ने क़ुबूल की और आज तक उसी राय के आधार पर पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर बयान हो रही है। इज्तिहाद जिस तरह शेष आदेशों में जारी है, उसी तरह तफ़सीरे-क़ुरआन करने में भी जारी है। जो व्यक्ति सही राय पर पहुँच जाएगा, उसे दो अज्र (प्रतिदान) मिलेंगे और जो ग़लती कर जाएगा, उसके लिए एक अज्र है। पवित्र क़ुरआन में चिन्तन-मनन और बुद्धि पर जो ज़ोर दिया गया है, वह इसी वजह से है। चिन्तन-मनन वहीं होता है जहाँ क़ुरआन या हदीस में स्पष्ट आदेश नहीं होता। इसलिए बज़ाहिर बाद के विद्वानों का यह दृष्टिकोण सही मालूम होता है कि वह राय जिसका आधार इज्तिहाद और अन्तर्दृष्टि पर हो, वह राय जिसका आधार शरीअत के आम आदेशों पर हो, वह राय जो अरबी भाषा एवं साहित्य के व्याकरण एवं सिद्धांतों के अनुकूल हो, और वह राय जिससे इस्लाम की आम परिकल्पना पर चोट न पड़ती हो, वह राय स्वीकार्य है, और उसके आधार पर पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर की जानी चाहिए। इमाम ग़ज़ाली ने ‘इहयाउल-उलूम’ में इस विषय पर पूरा एक अध्याय बाँधा है और ज़ोर-शोर से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है।
कम-से-कम एक उदाहरण अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने का भी मिलता है, जब उन्होंने अपने इज्तिहाद और अन्तर्दृष्टि के अनुसार पवित्र क़ुरआन के एक शब्द की तफ़सीर की। पवित्र क़ुरआन में ‘कलाला’ का शब्द प्रयुक्त हुआ है। ‘कलाला’ शब्दकोश में इस व्यक्ति को कहते हैं जिसके न माँ-बाप ज़िंदा हों और न कोई सन्तान हो, यानी उसको कोई विरासत देनेवाला हो और न उसकी विरासत लेनेवाला हो। ऊपर और नीचे के रिश्ते मौजूद न हों। आस-पास के रिश्ते हों जैसे बहन-भाई आदि। यह शब्द क़ुरैश की ज़बान में प्रचलित नहीं था। यह किसी अन्य क़बीले का शब्द था। इससे चूँकि अर्थ पूरी तरह अदा हो रहा था, इसलिए पवित्र क़ुरआन ने इस सन्दर्भ में इस शब्द को प्रयुक्त किया। क़ुरैश और हिजाज़ के लोगों को आम तौर पर ‘कलाला’ का अर्थ मालूम नहीं था। किसी ने अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी तरफ़ से इसका अर्थ बयान कर देता हूँ, अगर सही है तो अल्लाह तआला की ओर से है, और अगर ग़लत है तो मेरी और शैतान की ओर से। फिर उन्होंने ‘कलाला’ का यह अर्थ बयान किया जो मैंने अभी बताया।
समय बीतने के साथ-साथ तफ़सीर-बिर्राय की प्रवृत्ति बढ़ती गई और हर आनेवाला क़ुरआन का मुफ़स्सिर (टीकाकार) पिछले मुफ़स्सिरीन की तुलना में तफ़सीर-बिर्राय से अधिक काम लेने लगा। इसकी बड़ी वजह यह मालूम होती है कि तफ़सीर बिल-मासूर की पूरी सामग्री पूर्ण हो चुकी थी, अब इस सामग्री में कोई और बढ़ोतरी संभव नहीं थी। भाषा और साहित्य से संबंधित जो सामग्री थी वह भी सारी इकट्ठा हो चुकी थी। उसमें भी अब कोई वृद्धि संभव नहीं थी। अब इल्मे-तफ़सीर में तदधिक फैलाव जो हो सकता है वह तफ़सीर-बिर्राय या तफ़सीर-बिल-इज्तिहाद ही के आधार पर हो सकता है। शेष जितनी प्रवृत्तियों का आगे चलकर ज़िक्र किया जाएगा वे सब की सब तफ़सीर-बिर्राय या तफ़सीर-बिल-इज्तिहाद ही की कटैगरी में आती हैं।
तफ़सीर-बिर्राय की टीकाकारों ने पाँच शर्तें बयान की हैं, जिनका मैं संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर चुका हूँ। एक तो यह है कि यह तफ़सीर अरब शायरी एवं साहित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो, यानी अरबी भाषा के व्याकरण, भाषा शैलियोँ, हिजाज़ की दिनचर्या तथा मुहावरे के अनुसार किसी आयत या शब्द का वही मतलब निकलता हो जो टीकाकार ने बयान किया है। अगर अरबी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से वह अर्थ न निकलता हो और आप ज़बरदस्ती वह अर्थ निकालें जो आपका मन पसंद हो तो यह पथभ्रष्टता और विमुखता है। दूसरी और तीसरी शर्त यह कि इस तफ़सीरी राय की क़ुरआन और हदीस से अनुकूलता ज़रूरी है। अगर तफ़सीर-बिर्राय पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में बताए गए उसूलों के समरूप और इस्लाम की सर्वसम्मत शिक्षाओं के अनुसार है तो स्वीकार्य है। और अगर नहीं है तो ऐसी तफ़सीर को रद्द किया जाना चाहिए। चौथी शर्त यह कि तफ़सीर की जो आम शर्तें मुफ़स्सिरीन ने बयान की हैं कि कौन-सा शब्द ख़ास है कौन-सा आम है, कौन-सा नासिख़ (रद्द करनेवाला) है और कौन-सा मनसूख़ (रदद् किया हुआ), फिर कब और कहाँ कोई शब्द ख़ास है और कहाँ आम है। कहाँ पहले है और कहाँ बाद में है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। और पाँचवीं शर्त यह है कि जिन मामलों में इजमा-ए-उम्मत (मुस्लिम विद्वानों का मतैक्य) हो चुका है उनको नए सिरे से न छेड़ा जाए, और पवित्र क़ुरआन की सार्थकता और क्रमबद्धता को बरक़रार रखा जाए। इन पाँच चीज़ों की पाबंदी के साथ जो राय दी जाएगी वह स्वीकार्य होगी और तफ़सीरे-क़ुरआन में उससे काम लिया जाएगा।
जब यह प्रवृत्ति परिपक्व हो गई कि इन शर्तों के अनुसार अपनाई जानेवाली राय और इज्तिहाद के आधार पर तफ़सीर लिखी जा सकती है तो शोध और चिन्तन-मनन के बहुत-से नए दरवाज़े खुल गए। इस तरह और बहुत-सी तफ़सीरी प्रवृत्तियाँ पैदा हुईं। जिनमें से एक बहुत नुमायाँ प्रवृत्ति फ़िक़्ही तफ़सीरों की है। यानी पवित्र क़ुरआन की उन आयतों की विशेष तफ़सीर जहाँ फ़िक़्ही आदेश बयान हुए हैं। इस मामले में पहल करने का सौभाग्य किसे प्राप्त है, यह कहना बहुत मुश्किल है। इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी (रहमतुल्लाह अलैह) जो इमाम अबू-हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) के ख़ास शागिर्द हैं, उनकी किताबों में पवित्र क़ुरआन की फ़िक़्ही तफ़सीर पर भी बहुत-सी बहसें मिलती हैं। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) की मशहूर किताब ‘अल-मुदव्वना अल-कुबरा’ में पवित्र क़ुरआन की फ़िक़्ही तफ़सीर के इशारे मिलते हैं, मगर जिस मुफ़स्सिर को एक अलग और स्थायी रूप से फ़िक़ही तफ़सीर लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) थे, जिनकी किताब ‘अहकामुल-क़ुरआन’ दो भागों में मौजूद है और आज भी मिलती है। उनकी एक और किताब ‘अहकामुल-हदीस’ भी है। इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) ने पवित्र क़ुरआन की उन तमाम आयतों को जिनसे फ़िक़्ही आदेश निकलते हैं, अपनी ख़ास अलग शैली के अनुसार संकलित किया है और उनसे वे आदेश निकाले हैं जो आज फ़िक़्ह शाफ़िई का आधार हैं। इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) का अंदाज़ कभी-कभी बहुत अजीब और दिलचस्प होता है। न केवल उनका, बल्कि उनके ज़माने के अधिकतर मुफ़स्सिरीन और मुहद्दिसीन का यह अन्दाज़ था कि वह एक ज्ञानपरक संवाद या विचारों के आदान-प्रदान के अंदाज़ में बात करते हैं। ख़ास तौर पर फ़िक़्ही तफ़सीरों के अध्याय में, इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) अपने शिष्यों से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं कि यह आयत अमुक फ़िक़्ही आदेश पर आधारित है। मैंने इससे यह राय क़ायम की है। शिष्य उनसे मतभेद भी करते। इमाम साहब जवाब देते। फिर शिष्य आपत्ति करते और इमाम साहब जवाब देते। इस तरह बहस चलती। अगर सर्वसहमति हो गई तो लिख दी जाती और अगर मतभेद चलता रहता तो वह भी लिख दिया जाता। कभी-कभी बाहर से कोई फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) आता तो उससे भी बहस होती। वह भी लिख ली जाती, और इस तरह बहस पूरी हो जाती। इस तरह उनकी बहसें इमाम मुहम्मद (रहमतुल्लाह अलैह) से भी हुईं, इमाम अबू-यूसुफ़ (रहमतुल्लाह अलैह) से भी हुईं और अपने शिष्यों से भी हुईं। यह एक मुनाज़राना (शास्त्रार्थ जैसा) अंदाज़ होता था।
यह सिलसिला कमो-बेश सौ साल जारी रहा और एक-एक चीज़ स्पष्ट होकर सामने आ गई कि पवित्र क़ुरआन की फ़िक़्ही तफ़सीर की यह शैली है। पवित्र क़ुरआन की फ़िक़्ही तफ़सीर में जिस चीज़ से ज़्यादा काम लिया गया, वह निश्चय ही पवित्र क़ुरआन की आयतों और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्लम) की हदीसें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सिलसिले में अरबी भाषा की शैलियोँ और नियमों एवं सिद्धांतों से भी काम लिया गया। सबसे पहले यह देखने की कोशिश की गई कि कोई शब्द किसी ख़ास अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तो फिर उसी अर्थ को आधार बनाया जाए। कभी-कभी किसी शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक क़बीले की भाषा में एक अर्थ है और दूसरे क़बीले के मुहावरे में दूसरा अर्थ है। अगर ऐसा हो तो देखा जाएगा कि किस क़बीले की भाषा अधिक विश्वसनीय समझी जाती थी। यों फ़िक़्ही तफ़सीर के इस कार्य में भाषागत बहसें भी शामिल हो जाएँगी।
इमाम शाफ़िई (रहमतुल्लाह अलैह) की ‘अहकामुल-क़ुरआन’ के बाद फ़िक़्ही तफ़सीर के अध्याय में चार किताबों का ज़िक्र मैं और करता हूँ — दो किताबों का भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर की और दो किताबों का भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर से — भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फ़िक़्ही तफ़सीरों के विषय में दो किताबें बहुत मशहूर और नुमायाँ हैं। एक किताब फ़िक़्ह हनफ़ी की रौशनी में संकलित हुई। और मशहूर हनफ़ी फ़क़ीह इमाम अबू-बक्र जस्सास की संकलित की हुई है। उनकी किताब का नाम है ‘अहकामुल-क़ुरआन’। इस किताब में उन्होंने आदेशवाली तमाम आयतों को जमा करके उनकी फ़िक़्ही तफ़सीर की है। वह अधिकतर आयतों की तफ़सीर करते हैं। उनकी दिलचस्पी और ध्यान का विषय केवल आदेशोंवाली आयतें हैं। इमाम जस्सास की किताब फ़िक़्ही तफ़सीर के साहित्य में बहुत उच्च स्थान रखती है। इमाम साहब ख़ुद एक प्रसिद्ध फ़क़ीह और माहिरे-उसूल भी थे। उन्होंने उसूले-फ़िक़्ह पर जो किताब लिखी थी वह हनफ़ी दृष्टिकोण से उसूले-फ़िक़्ह की सर्वप्रथम और उत्तम किताबों में से है। इमाम साहब ने अपनी इस तफ़सीर में इल्म उसूले-फ़िक़्ह के नियमों को भी चस्पाँ करके दिखाया है। इस किताब का अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी में उर्दू में अनुवाद हो चुका है और प्रकाशित भी हो गया है।
दूसरी किताब भी ‘अहकामुल-क़ुरआन’ ही के नाम से है। यह एक मालिकी फ़क़ीह क़ाज़ी अबू-बक्र-बिन-अल-अरबी मालिकी की रचना है। क़ाज़ी साहब उंदलुस के रहनेवाले थे। उनकी यह किताब अरबी में है और आम मिलती है। इसको आप इमाम जस्सास की उक्त किताब की मालिकी बहन कह सकते हैं। इन दोनों की तुलना पर भी काफ़ी काम हुआ है। एक साहब को हमने इस विषय पर अपनी यूनिवर्सिटी में पी.एचडी करने के लिए विषय दिया है जिसमें वह दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताएँगे कि इन दोनों के तर्क करने का अंदाज़ क्या है। फ़िक़्ही तफ़सीरों में एक और महत्त्वपूर्ण किताब, यानी अल्लामा क़ुर्तुबी की ‘अहकामुल-क़ुरआन’ का मैं पहले उल्लेख चुका हूँ।
भारतीय उपमहाद्वीप में दो उल्लेखनीय तफ़सीरें फ़िक़्ही अंदाज़ की लिखी गईं। एक थी ‘अत-तफ़सीरातुल-अहमदिया’। मुल्ला अहमद जीवन के नाम से भारत में एक बुज़ुर्ग थे, औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। यह बुज़ुर्ग अमेठी के रहनेवाले थे और मूलतः फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह के विशेषज्ञ थे। तफ़सीराते-अहमदिया को ख़ुदा-ना-ख़ास्ता क़ादियानियों से संबद्ध न कीजिएगा, उनका नाम अहमद था और उन्होंने इस किताब को अपने नाम से संबद्ध किया। इस किताब में उन्होंने फ़िक़्ही आयतों की तफ़सीर लिखी है। किताब संक्षिप्त और एक भाग में है, लेकिन लेखक के ज्ञान की विशालता और गहराई को प्रकट करती है।
फ़िक़्ही तफ़सीर के मैदान में एक और किताब है जो ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है। उसे विद्वानों की एक टीम ने तैयार किया था। मौलाना अशरफ़ अली थानवी जो भारतीय उपमहाद्वीप के मशहूर मुफ़स्सिरे-क़ुरआन भी हैं, उन्हें यह ख़याल आया कि हनफ़ी दृष्टिकोण से पवित्र क़ुरआन की कोई सारगर्भित फ़िक़्ही तफ़सीर नहीं है। ऐसी फ़िक़्ही तफ़सीर जिसमें पवित्र क़ुरआन की आरंभ से आख़िर तक लगातार तफ़सीर भी की गई हो और हनफ़ी फ़क़ीहों के तर्क भी इसमें विस्तार से एकत्र कर दिए गए हों। इस मक़सद के लिए उन्होंने अपने शिष्यों की जो अपनी-अपनी जगह बड़े विद्वान थे एक टीम तैयार की और पवित्र क़ुरआन के विभिन्न भाग उनके ज़िम्मे लगाए कि वे इस काम को करें। इस टीम में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना मुफ़्ती शफ़ी, मौलाना मुहम्मद इदरीस कांधलवी और मौलाना मुफ़्ती जमील अह्मद जैसे बड़े विद्वान शामिल थे। लगभग 60-65 वर्ष के समय में यह किताब पूरी हो गई। लेकिन इसके विभिन्न अंश अलग-अलग प्रकाशित हुए। कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में। कुछ बाद, में कुछ पहले। अगर इन सबको इकट्ठा किया जाए तो यह शायद पच्चीस-तीस भागों पर सम्मिलित एक किताब बनेगी। अतीत में इसके आख़िरी अंश भी पूरे हो गए हैं। इसमें पूरे पवित्र क़ुरआन की फ़िक़्ही तफ़सीर को पूरा किया गया है। और इसका नाम भी ‘अहकामुल-क़ुरआन’ है। हनफ़ी फ़क़ीहों का दृष्टिकोण जो पहले बहुत-सी किताबों में बिखरा हुआ था, अब बड़ी हद तक एक जगह सामने आ जाता है। ज्ञानपरक दृष्टि से यह एक मूल्यवान काम है।
फ़िक़्ही प्रवृत्ति के बाद एक बड़ी प्रवृत्ति वैचारिक और धारणात्मक पैदा हुई। हर वर्ग ने यह प्रयास किया कि अपने अक़ीदों (धारणाओं) के आधार पर एक तफ़सीर संकलित करे और अपने तर्क उसमें बयान कर दे। यह कोशिश इस दृष्टि से बहुत सकारात्मक और सुखद थी कि मुसलमानों में कोई वर्ग और फ़िर्क़ा ऐसा नहीं हुआ, जिसने अपने मज़हबी अक़ीदे का आधार पवित्र क़ुरआन के अलावा किसी और चीज़ पर रखा हो। मतभेद से अलग हटकर इससे यह बात ज़रूर पता चलती है कि मुसलमानों का हर फ़िर्क़ा अपने अक़ीदों का आधार पवित्र क़ुरआन ही पर रखता है जो एक साझी चीज़ है। आप किसी फ़िर्क़े के अर्थ या व्याख्या से सहमत हों या असहमत हों, वह अलग चीज़ है, लेकिन सबका आधार पवित्र क़ुरआन ही है।
कलामी तफ़सीरों में कुछ किताबें तो वे हैं जो अहले-सुन्नत के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। फिर अहले-सुन्नत में कलामी दृष्टिकोण से कई प्रवृत्तियाँ थीं। आपने हम्बली, अशअरी और मातुरीदी का ज़िक्र सुना होगा। ये तीनों अक़ीदों में अहले-सुन्नत के तीन मकातिबे-फ़िक्र (Schools of thoughts) या प्रवृत्तियाँ हैं। इन सबके बारे में अलग-अलग किताबें लिखी गईं। इमाम अबू-मंसूर मातुरीदी जिनका संबंध मध्य एशिया से था, उनकी किताब है ‘तावीलाते-अहले-सुन्नः’। यह पवित्र क़ुरआन की बड़ी मोटी तफ़सीर है। इसी तरह इमाम राज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) जो शाफ़िई भी थे और अशअरी भी। उन्होंने अपने अक़ीदों के दृष्टिकोण से काम किया और अशअरी अक़ाइद के आधार यह तफ़सीर लिखी है। जमख़्शरी का हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। जो मोतज़िली थे। उन्होंने जहाँ पवित्र क़ुरआन के साहित्यिक और भाषागत सौंदर्य को बयान किया है वहाँ मोतज़िली अक़ीदों का समर्थन भी किया है। इमाम शौकानी (रहमतुल्लाह अलैह) का मैंने पहले उल्लेख किया, जो फ़िर्क़ा जै़दिया से संबंध रखते थे। उन्होंने ‘फ़तहुल-क़दीर’ में अपने अक़ीदों की व्याख्या ज़ैदी दृष्टिकोण से की है।
मोतज़िली फ़िर्क़े में एक और तफ़सीर बहुत अलग है। वह क़ाज़ी अबदुल-जब्बार की है। क़ाज़ी अबदुल-जब्बार एक प्रसिद्ध विद्वान थे और मोतज़िला के दृष्टिकोण से पहली पंक्ति के विद्वान और शोधकर्ता समझे जाते थे। मोतज़िला के यहाँ जब कहा जाए कि क़ाज़ी अल-क़ज़ा ने यह कहा तो इससे अभिप्रेत क़ाज़ी अबदुल-जब्बार मोतज़िली ही होते हैं। उनकी एक किताब है जो बहुत असाधारण हैसियत रखती है, और वह है तंज़ीहुल-क़ुरआन अनिल-मताइन’ यानी पवित्र क़ुरआन का बचाव विभिन्न आपत्तियों से। इस तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त किताब में उन्होंने ग़ैर-मुस्लिमों और नास्तिकों की पवित्र क़ुरआन पर आपत्तियों का जवाब दिया है। लेकिन चूँकि वे ख़ुद मोतज़िली हैं इसलिए मोतज़िली दृष्टिकोण से उन्होंने ये जवाब दिए हैं। कुछ जगह उनके जवाब असाधारण महत्त्व रखते हैं। इसी तरह शीया लोगों की भी बहुत-सी तफ़सीरें हैं जिनमें पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर शीया अक़ीदों के दृष्टिकोण से की गई है। उनमें से एक तफ़सीर जो बहुत सन्तुलित और मध्यमार्गी मानी जाती है वह ‘मजमउल-बयान’ है, जो अल्लामा अबू-अली तबरसी की है। यह किताब 10 भागों में तेहरान और बेरूत आदि से कई बार प्रकाशित हुई है। यह जामिआ अज़हर की एक उपसंस्था है जिसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न इस्लामी फ़िक़्हों और फ़िर्क़ों में निकटता पैदा की जाए। इस संस्था ने इस तफ़सीर को बहुत मध्यमार्गी और सन्तुलित पाया तो नमूने के तौर पर इस तफ़सीर को प्रकाशित किया कि तफ़सीर में मध्यमार्गी प्रवृत्ति ऐसे पैदा हो सकती है।
निश्चय ही इस किताब में शीया अक़ीदे और धारणाएँ ही बयान की गई हैं, लेकिन कई पहलुओं से यह किताब एक ख़ास ज्ञानपरक महत्त्व रखती है। और इसमें बहुत-सी ज्ञानपरक सामग्री शामिल है। सूरतों का गठन और आयतों के उचित होने पर बहुत-सी नई बातें हैं। लेकिन इस किताब के बारे में मैंने एक दिलचस्प घटना पढ़ी है। मालूम नहीं वह ऐतिहासिक रूप से दुरुस्त है या ग़लत। वह यह कि अपनी नौजवानी में यह लेखक सकते का शिकार हो गए थे। लोगों ने मुर्दा समझकर दफ़न कर दिया। जब सकते की कैफ़ियत ख़त्म हुई और पता चला कि क़ब्र में दफ़न हैं तो बहुत डरे और अल्लाह तआला से दुआ की कि या अल्लाह अगर यहाँ से निकल जाऊँ तो शुक्र के तौर पर पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर करूँगा। इसी दौरान में एक कफ़न-चोर आ गया। उसने कफ़न चोरी के उद्देश्य से क़ब्र खोदी। अंदर से यह ज़िंदा बरामद हुए तो वह डर गया। लेकिन उन्होंने उसे बहुत कुछ इनाम देकर रुख़स्त किया और बाद में यह तफ़सीर लिखी। यह घटना उनके बारे में मशहूर है।
इसके बाद एक बड़ी प्रवृत्ति सूफ़ियाना तफ़सीर की पैदा हुई जिसमें सूफ़ी लोगों ने अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पवित्र क़ुरआन की तफ़सीरें लिखीं। उदाहरणार्थ आलूसी की तफ़सीर में भी सूफियाना अंदाज़ है। मौलाना जलालुद्दीन रुमी की मसनवी में भी बहुत-सी सूफ़ियाना सामग्री मिलती है जिनमें उन्होंने बहुत-सी क़ुरआनी आयतों की सूफ़ियाना अंदाज़ से तफ़सीर की है।
एक आख़िरी किताब जो सूफियाना प्रवृत्ति रखती है, मौलाना अशरफ़ अली थानवी की एक संक्षिप्त किताब है जो उनकी तफ़सीर ‘बयानुल-क़ुरआन’ के एक हिस्से के तौर पर प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने वे तमाम उसूल जो तसव्वुफ़ में बरते जाते हैं, उनका पवित्र क़ुरआन से मूलस्रोत तलाश करने की कोशिश की है। यह किताब अलग से भी प्रकाशित हुई है।
एक और प्रवृत्ति जो बीसवीं सदी ईस्वी में बहुत नुमायाँ हुई वह वैज्ञानित तफ़सीर की प्रवृत्ति थी। अगरचे पवित्र क़ुरआन न विज्ञान की किताब है और न चिकित्सा की। लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि पवित्र क़ुरआन में वैज्ञानिक प्रकार के वक्तव्य भी आए हैं इसलिए उनपर भी अलग से शोध की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सबसे नुमायाँ काम मिस्र के अल्लामा तनतावी जौहरी का है। अल्लामा जौहरी ने ‘जवाहरुल-क़ुरआन’ के नाम से एक बहुत विस्तृत तफ़सीर लिखी। इसमें उन्होंने पवित्र क़ुरआन की वैज्ञानिक ढंग से टीका लिखने की कोशिश की है। उनके ज़माने तक जितना वैज्ञानिक विकास हुआ था, उन्होंने उस किताब में उस सबसे काम लिया है। और कोशिश की है कि यह दिखाएँ कि क़ुरआन में जितने वैज्ञानिक वक्तव्य आए हैं उनका अब तक के अनुभवों और वैज्ञानिक शोधों से समर्थन हो गया है।
अधिकतर मुस्लिम विद्वान इससे सहमत नहीं होते। मुझे भी इस शैली से सहमति नहीं है। पवित्र क़ुरआन विज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन के लिए उतारी गई है। यह किताब इंसानों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए अवतरित की गई है। पवित्र क़ुरआन का यह उद्देश्य नहीं है कि वह इंसानी आविष्कारों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करे। इस काम के लिए अल्लाह की ओर से वह्य अवतरित करने की ज़रूरत नहीं थी। वह्य (ईश-प्रकाशना) की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ मानव बुद्धि और अनुभव काम न कर सके। अब अगर ज़बरदस्ती किसी वैज्ञानिक प्रयोग को क़ुरआन के साथ मिला दें और 50 साल बाद वह वैज्ञानिक प्रयोग ग़लत साबित हो तो फिर आप क्या कहेंगे?
एक आख़िरी प्रवृत्ति जिसकी ओर संक्षिप्त इशारा करना काफ़ी है, यह है कि जब पवित्र क़ुरआन की तफ़सीर की सारी सामग्री इकट्ठी हो गई और सारगर्भित तफ़सीरें लिखी जाने लगीं तो इस बात की ज़रूरत पड़ी कि विभिन्न विषयों पर अलग-अलग भी पवित्र क़ुरआन की तफ़सीरें आनी चाहिएँ। इसको तफ़सीरे-मौज़ूई (विषयगत टीका) कहते हैं। उदाहरणार्थ क़ुरआन में बयान क़िस्सों पर अलग किताबें, क़ुरआन में वर्णित भूगोल पर अलग किताबें। इस तरह की तफ़सीरों की संख्या इतनी अधिक है कि ऐसी किताबों की संख्या हज़ारों में है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जरमन, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें पवित्र क़ुरआन के विभिन्न विषयों पर अलग-अलग किताबें न लिखी गई हों। उनमें से किसी एक किताब को प्रतिनिधि की हैसियत देना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ऐसी किताबें भी अनगिनत हैं जिनमें से हर एक अलग हैसियत रखती है। यह वह प्रवृत्ति है जो आजकल भी ज़ोर-शोर से जारी है, और जब से यह प्रवृत्ति आरंभ हुई है, उसमें लगातार वृद्धि होती चली गई है। दस-बारह वर्ष पूर्व यूनेस्को ने एक योजना बनाई थी कि पवित्र क़ुरआन के मूल विषयों पर एक सारगर्भित किताब तैयार कराई जाए। हमारे मुहतरम साथी डॉक्टर ज़फ़र इसहाक़ अंसारी यूनेस्को की ओर से इस प्राजेक्ट के जनरल एडिटर हैं। उन्होंने यह काम बड़े पैमाने पर दुनिया-भर के विद्वानों से करवाया है।
इस उदाहरण से यह बताना अभीष्ट है कि ग़ैर-मुस्लिमों की संस्थाएँ भी पवित्र क़ुरआन की विषयगत तफ़सीर में दिलचस्पी रखती हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं।
यह तफ़सीर की बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें संक्षेप के साथ पेश किया गया है।
Facebook: HindiIslam,Twitter: HindiIslam1, YouTube: HindiIslamTv, E-Mail: HindiIslamMail@gmail.com)
Recent posts
-
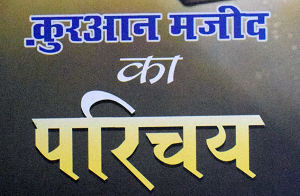
क़ुरआन मजीद का परिचय
29 April 2024 -

क़ुरआन की शिक्षाएँ मानवजाति के लिए अनमोल उपहार
27 March 2024 -

पवित्र क़ुरआन की शिक्षा : आधुनिक समय की अपेक्षाएँ (क़ुरआन लेक्चर -12)
12 December 2023 -

पवित्र क़ुरआन का विषय और महत्त्वपूर्ण वार्त्ताएँ (क़ुरआन लेक्चर - 11)
12 December 2023 -

नज़्मे-क़ुरआन और क़ुरआन की शैली (क़ुरआन लेक्चर- 10)
12 December 2023 -

उलूमुल-क़ुरआन-क़ुरआन से संबंधित ज्ञान (क़ुरआन लेक्चर - 9)
12 December 2023